
जिहाद की वास्तविकता
-
इस्लाम
- at 15 March 2020
मानव-सभ्यता एवं नागरिकता की आधारशिला जिस क़ानून पर स्थित है उसकी सबसे पहली धारा यह है कि मनुष्य की जान और उसका रक्त सम्माननीय है। मनुष्य के नागरिक अधिकारों में सर्वप्रथम अधिकार जीवित रहने का अधिकार है और नागरिक कर्तव्यों में सर्वप्रथम कर्तव्य जीवित रहने देने का कर्तव्य है। संसार के जितने धर्म-विधान और सभ्य विधि-विधान हैं, उन सब में जान के सम्मान का यह नैतिक नियम अवश्य पाया जाता है। जिस क़ानून और धर्म में इसे स्वीकार न किया गया हो, वह न तो सभ्य लोगों का धर्म और क़ानून बन सकता है, न उसके अन्तर्गत कोई मानव-समुदाय शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और न ही उसे कोई उन्नति प्राप्त हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो मानव जान की इस गरिमा का आदर न करें और अपने स्वार्थ में दूसरे मनुष्य की हत्या करने लगें और धरती पर बिगाड़ फैला कर रख दें ऐसे लोगों को रोकना और दंडित करना ज़रूरी है। ज़मान को बिगाड़ से बचाने के लिए, इस्लाम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की अनुमति देता है। जिहाद का अर्थ होता है सतत प्रयास करना और अगर ज़रूरी हो तो इसके लिए तलवार भी उठाई जा सकती है।
जिहाद: मानव-जान का सम्मान
मानव-सभ्यता एवं नागरिकता की आधारशिला जिस क़ानून पर स्थित है उसकी सबसे पहली धारा यह है कि मानव-जान और उसका रक्त सम्माननीय है। मानव के नागरिक अधिकारों में सर्वप्रथम अधिकार जीवित रहने का अधिकार है और नागरिक कर्तव्यों में सर्वप्रथम कर्तव्य जीवित रहने देने का कर्तव्य है। संसार के जितने धर्म-विधान और सभ्य विधि-विधान हैं, उन सब में जान के सम्मान का यह नैतिक नियम अवश्य पाया जाता है। जिस क़ानून और धर्म में इसे स्वीकार न किया गया हो, वह न तो सभ्य लोगों का धर्म और क़ानून बन सकता है, न उसके अन्तर्गत कोई मानव-दल शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है और न ही उसे कोई उन्नति प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समझ सकता है कि यदि मानव-जान का कोई मूल्य न हो, उसका कोई सम्मान न हो, उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध न हो तो चार आदमी कैसे मिलकर रह सकते हैं, उनमें किस तरह परस्पर कारोबार हो सकता है, उन्हें वह शान्ति एवं परितोष और वह निश्चिन्तता तथा चित्त की स्थिरता कैसे प्राप्त हो सकती है, जिसकी मनुष्य को व्यापार, कला और कृषि-कार्य, धनार्जन, गृह-निर्माण, यात्र एवं पर्यटन और सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता होती है। फिर यदि आवश्यकताओं से हटकर मात्र मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो इस दृष्टि से भी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण अपने एक भाई की हत्या करना निकृष्टतम निर्दयता और अत्यंत पाषाण हृदयता है। ऐसा अपराध करके मानव में किसी नैतिक उच्चता का पैदा होना तो अलग रहा, उसका मानवता के स्तर पर स्थित रहना भी असंभव है।
संसार के राजनैतिक क़ानून तो मानव-जीवन के सम्मान को केवल दंड के भय और शक्ति के बाल पर स्थापित करते हैं। किन्तु एक सत्यधर्म का काम दिलों में उसका वास्तविक मान-सम्मान पैदा कर देना है, ताकि जहाँ मानव द्वारा दिए जाने वाले दंड का भय न हो और जहाँ मनुष्य को पुलिस रोकने के लिए न हो वहाँ भी लोग एक-दूसरे की अकारण हत्या करने से बचते रहें। इस दृष्टिकोण से जान-सम्मान की जैसी यथोचित और प्रभावकारी शिक्षा इस्लाम में दी गई है वह किसी दूसरे धर्म में मिलनी कठिन है। क़ुरआन में जगह-जगह विभिन्न ढंग से इस शिक्षा को दिलों में बिठाने की कोशिश की गई है। क़ुरआन सूरा-5 अल-माइदा में आदम (अलैहि॰) के दो बेटों का क़िस्सा बयान करके, जिनमें से एक ने दूसरे की हत्या की थी और यह हत्या मात्र अत्याचार था, कहा गया है :
‘‘इसी कारण इसराईल की संतान के लिए हमने यह आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान किया। मगर उनका हाल यह है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले-खुले निर्देश लेकर आये, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं।’’ (कु़रआन, 5:32)
एक दूसरी जगह ईश्वर ने अपने नेक बन्दों के गुण बयान करते हुए कहा है :
‘‘ईश्वर के वर्जित किए हुए किसी जीव का नाहक़ क़त्ल नहीं करते, और न व्यभिचार करते हैं—ये काम जो कोई करेगा वह अपने गुनाह का बदला पाएगा।’’ (कु़रआन, 25:68)
एक और जगह कहा है:
‘‘ऐ नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे रब ने तुम पर क्या-क्या पाबन्दियाँ लगाई हैं: यह कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ, और माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो और अपनी औलाद को निर्धनता के भय से क़त्ल न करो। हम तुमको भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे, और अश्लील बातों के क़रीब भी न जाओ चाहे वे खुली हुई हों या छिपी। और किसी जीव की, जिसे ईश्वर ने आदरणीय ठहराया है, हत्या न करो, सिवाय इस स्थिति के कि ऐसा करना सत्य को अपेक्षित हो। ये बातें हैं जिनका आदेश उसने तुम्हें दिया है, ताकि तुम समझ-बूझ से काम लो।’’ (कु़रआन, 6:151)
इस शिक्षा का संबोधन सर्वप्रथम उन लोगों से था जिनकी दृष्टि में मानव-जान का कोई मूल्य नहीं था और जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए संतान तक की हत्या कर दिया करते थे। इसलिए इस्लाम की ओर बुलाने वाले पैग़म्बर (उन पर हज़ारों-हज़ार सलाम हों) उनकी मनोवृत्तियों के सुधार के लिए स्वयं भी सदैव जान-सम्मान का उपदेश दिया करते थे और यह उपदेश सदैव अत्यंत प्रभावकारी शैली में हुआ करता था। हदीसों में अधिकतर इस प्रकार के कथन पाए जाते हैं जिनमें निर्दोष की हत्या को निकृष्टतम पाप बताया गया है। उदाहरणस्वरूप कुछ हदीसें हम यहाँ उद्धृत करते हैं:
हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा:
‘‘बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ईश्वर का सहभागी ठहराना है और जीव-हत्या तथा माता-पिता की अवज्ञा एवं झूठ बोलना है।’’
हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा:
‘‘ईमान वाला अपने धर्म की विस्तीर्णता में उस समय तक निरंतर रहता है जब तक वह कोई अवैध रक्त-पात नहीं करता।’’
हदीसशास्त्र ‘नसई’ में एक ‘मुतवातिर’1 (वह हदीस जिसके उल्लेखकर्ता हर ज़माने में इतने अधिक रहे हों कि उनका किसी झूठ पर सहमत हो जाना संभव न हो।) हदीस है कि ‘‘क़ियामत (प्रलय-दिवस) के दिन बन्दे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, वह नमाज़ है और पहली चीज़ जिसका निर्णय लोगों के मध्य किया जाएगा, वे ख़ून के दावे हैं।’’
एक बार एक व्यक्ति हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने पूछा, ‘‘सबसे बड़ा गुनाह कौन-सा है?’’ हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने जवाब दिया, ‘‘यह कि तू किसी को ईश्वर का समकक्ष एवं प्रतिद्वंद्वी ठहराए, जबकि उसने तुझे पैदा किया।’’
उसने फिर पूछा कि, ‘‘इसके बाद कौन-सा गुनाह बड़ा है?’’ पैग़म्बर (सल्ल॰) ने उत्तर दिया, ‘‘यह कि तू अपने बच्चे की हत्या कर दे, इस विचार से कि वह तेरे खाने में साझीदार होगा।’’
उसने कहा, ‘‘इसके बाद कौन-सा गुनाह है?’’ पैग़म्बर (सल्ल॰) ने कहा, ‘‘यह कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे।’’
संसार पर इस्लामी शिक्षा का नैतिक प्रभाव
जान-सम्मान की यह शिक्षा किसी दार्शनिक या नैतिक शिक्षक के चिंतन का परिणाम न थी कि इसका प्रभाव केवल पुस्तकों और पाठशालाओं तक सीमित रहता, बल्कि वास्तव में वह ईश्वर और उसके पैग़म्बर की शिक्षा थी जिसका एक-एक शब्द प्रत्येक मुसलमान के ईमान का अंश था, जिसका पालन करना, उपदेश देना और जिसे क्रियान्वित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य था जो इस्लाम के कलिमे (महावाक्य और इस्लामी धारणा) को स्वीकार करता हो। अतः एक चैथाई शताब्दी के अल्प समयम ही में इसके कारण अरब जैसी हिंसक जाति में जान-सम्मान और शान्तिप्रियता का ऐस गुण पैदा हो गया कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की भविष्यवाणी के अनुसार क़ादसिया से सनआ तक एक महिला अकेली सफ़र करती थी और कोई उसकी जान और माल पर हमला न करता था, जबकि यही वह देश था जहाँ 25 वर्ष पूर्व बड़े-बड़े क़ाफ़िले भी निश्चिन्त होकर नहीं गुज़र सकते थे। फिर जब सभ्य संसार का आधे से अधिक भाग इस्लामी राज्य के अधीन हो गया और इस्लाम के नैतिक प्रभाव संसार में चारों ओर फैल गए तो इस्लामी शिक्षा ने मनुष्य के बहुत-से भ्रष्टाचारों और गुमराहियों की तरह मानव-जान के उस निरादर का भी उन्मूलन कर दिया जो संसार में फैला हुआ था। आज संसार के सभ्य क़ानूनों में जान-सम्मान को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह उस क्रान्ति के परिणामों में से एक शानदार परिणाम है जो क्रान्ति इस्लामी शिक्षा के फलस्वरूप संसार के नैतिक वातावरण में आई थी। अन्यथा जिस अंधकारमय काल में यह शिक्षा अवतरित हुई थी उसमें मानव-जान का वास्तव में कोई मूल्य न था। अरब की हिंसक प्रवृत्तियों का नाम तो इस सिलसिले में दुनिया ने बहुत सुना है, किन्तु उन देशों की स्थिति भी कुछ अच्छी न थी जो उस समय संसार की सभ्यता, सुसंस्कृति और ज्ञान तथा दर्शन के केन्द्र बने हुए थे। रूम के कोलोसियम (Colosseum) की कहानियाँ अब तक इतिहास के पृष्ठों में मौजूद हैं, जिनमें हज़ारों मनुष्य तलवार चलाने की कला (Gladiatory) की कुशलताओं और रोम के सरदारों के मनोरंजन की भेंट चढ़ गए। अतिथियों के मनोरंजन के लिए या मित्रों के सत्कार के लिए ग़ुलामों को हिंसक पशुओं से फड़वा देना या पशुओं की तरह ज़बह (वध) करा देना या उनके जलने का तमाशा देखना यूरोप और एशिया के अक्सर देशों में कोई बुरा काम न था। क़ैदियों और ग़ुलामों को विभिन्न ढंग से यातना दे-देकर मार डालना उस युग की सामान्य रीति थी। जाहिल और हिंसक प्रवृत्ति के सरदारों ही में नहीं यूनान और रोम के बड़े-बड़े चिंतकों और दार्शनिकों तक के अनुशीलनों और निरूपणों में मनुष्य के निर्दोष वध करने की बहुत-सी असभ्य रीतियाँ वैध थीं। अरस्तू और प्लेटो जैसे नैतिक शिक्षक माता को यह अधिकार देने में कोई दोष नहीं समझते थे कि वह अपने शरीर के एक अंश (गर्भाशय में पलते हुए बच्चे) को अलग कर दे। अतएव यूनान और रोम में गर्भपात कराना कोई अवैध कर्म न था। पिता को अपनी संतान के वध का पूरा अधिकार था और रोम के क़ानूनविदों को अपने क़ानून की इस विशेषता पर गर्व था कि उसमें संतान पर पिता के अधिकार इतने अधिक असीम हैं। स्टोइक (Stoics) दार्शनिक की दृष्टि में मनुष्य का स्वयं अपने आपका वध करना कोई बुरा काम न था, बल्कि ऐसा श्रेष्ठ कार्य था कि लोग सभाएँ आयोजित करके उनमें आत्महत्याएँ किया करते थे। यहाँ तक कि प्लेटो जैसा दार्शनिक भी इसे कोई बहुत बड़ा पाप न समझता था। पति के लिए अपनी पत्नी का वध बिल्कुल ऐसा था जैसे वह अपने किसी पालतू पशु का वध कर दे। इसलिए यूनान के क़ानून में इसका कोई दंड न था। जीव-रक्षा का गहवारा भारत इन सबसे बढ़ा हुआ था। यहाँ पुरुष के शव पर जीवित स्त्री को जला देना एक वैध कर्म था और धर्म में इसकी ताकीद थी। शूद्र के जान का कोई मूल्य न था और केवल इस कारण कि वह बेचारा शूद्र ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुआ है, उसकी हत्या ब्राह्मण के लिए वैध थी। वेद की आवाज़ सुन लेना शूद्र के लिए इतना बड़ा पाप था कि उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे मार डालना न केवल वैध, बल्कि आवश्यक था। ‘जलबरदा’ की प्रथा सामान्य रूप से प्रचलित थी जिसके अनुसार माता-पिता अपने पहले बच्चे को गंगा नदी की भेंट चढ़ा देते थे और इस कठोर हृदयता को अपने लिए सौभाग्य समझते थे।
ऐसे अंधकारमय युग में इस्लाम ने आवाज़ बुलन्द की कि, ‘‘मानव-जान को ईश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है, उसकी हत्या न करो, किन्तु उस समय जबकि सत्य और न्याय उसकी हत्या की माँ करे।’’ (कु़रआन, 6:151) इस आवाज़ में एक शक्ति थी और शक्ति के साथ वह ‘अहिंसा परमो धर्मः’ (अहिंसा परम धर्म है) की आवाज़ की तरह बुद्धि और प्रकृति के प्रतिवू$ल न थी, इसलिए वह संसार के कोने-कोने में पहुँची और उसने मानव को अपने जान के यथोचित मूल्य से अवगत कराया। चाहे किसी जाति या किसी देश ने इस्लाम स्वीकार किया हो या न किया हो, उसका नैतिक जीवन किसी न किसी हद तक इस आवाज़ से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। सामाजिक इतिहास का कोई न्यायप्रिय विद्वान इससे इन्कार नहीं कर सकता कि संसार के नैतिक क़ानूनों में मानव-जान के सम्मान को प्रतिष्ठित रखने का गौरव जितना इस आवाज़ को प्राप्त है उतना ‘पहाड़ी के उपदेश’ या ‘अहिंसा परमो धर्मः’ की आवाज़ को प्राप्त नहीं है।
क़त्ल जब सत्य और न्याय को अपेक्षित हो
तनिक विचार कीजिए, केवल ‘‘मानव-जान की, जिसे ईश्वर ने प्रतिष्ठित ठहराया है, हत्या न करो’’ ही नहीं कहा, बल्कि इसके साथ ‘‘किन्तु उस समय जबकि सत्य और न्याय उसकी हत्या की माँग करे’’ भी कहा है। ‘‘जिसने एक व्यक्ति की हत्या की मानो कि उसने समस्त लोगों की हत्या कर दी’’ ही नहीं कहा, बल्कि इसके साथ ‘‘किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद फैलाने के अतिरिक्त’’ का अपवाद भी रखा है। यह नहीं कहा कि किसी जान का किसी स्थिति में भी वध न करो। ऐसा कहा जाता तो यह शिक्षा का दोष होता। न्याय न होता, बल्कि वास्तव में अन्याय होता। संसार को वास्तव में आवश्यकता इस बात की न थी कि मनुष्य को क़ानून की पकड़ से आज़ाद कर दिया जाए और उसे खुली छूट दे दी जाए कि जितना चाहे फ़साद करे, जितनी चाहे अशान्ति फैलाए, जितना चाहे अत्याचार करे, प्रत्येक स्थिति में उसके जान का सम्मान किया जाएगा (अर्थात् उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा)। बल्कि वास्तव में आवश्यकता यह थी कि संसार में शान्ति की स्थापना हो, बिगाड़ और उपद्रव का उन्मूलन कर दिया जाए और ऐसा क़ानून बनाया जाए जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में स्वतंत्र हो और कोई व्यक्ति एक निश्चित सीमा का उल्लंघन करके दूसरों की भौतिक या आध्यात्मिक शान्ति में विघ्न न डाले। इस उद्देश्य के लिए केवल ‘‘जीव-हत्या न करो’’ का समर्थन ही अपेक्षित न था, बल्कि इस रक्षक-शक्ति की भी आवश्यकता थी कि ‘‘यदि सत्य और न्याय को अपेक्षित हो’’ तो (अपराधी को) क़त्ल भी किया जा सकता है, अन्यथा शान्ति की जगह अशान्ति ही होती।
दुनिया का कोई क़ानून, जो कर्म के बदले के नियम से रिक्त हो, सफल नहीं हो सकता। मानव-प्रकृति इतनी आज्ञाकारी नहीं है कि जिस चीज़ का आदेश दिया जाए उसे सदा सहर्ष स्वीकार कर ही ले और जिस चीज़ से रोका जाए, उसे सहर्ष त्याग ही दे। यदि ऐसा होता तो संसार में उपद्रव और बिगाड़ नाममात्रा को न होता। मनुष्य की प्रकृति में तो भलाई के साथ बुराई और आज्ञापालन के साथ अवज्ञा भी पाई जाती है। अतः उसकी उद्दंड प्रकृति को आज्ञापालन पर बाध्य करने के लिए ऐसे क़ानून की आवश्यकता है जिसमें आदेश देने के साथ यह भी हो कि यदि आदेश का पालन न किया गया तो उसका दंड क्या है और वर्जित करने के साथ यह भी हो कि यदि वर्जित कर्म से बचा न गया तो उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। केवल ‘‘धरती के सुधार के बाद उसमें बिगाड़ पैदा न करो’’ या ‘‘जिस प्राणी को ईश्वर ने प्रतिष्ठित किया है उसकी हत्या न करो’’ कहना पर्याप्त नहीं हो सकता, जब तक कि इसके साथ यह भी न बता दिया जाए कि यदि इस महापाप से किसी ने अपने को दूर न रखा और फ़साद फैलाया और रक्तपात किया तो उसे क्या दंड दिया जाएगा।
मानव-शिक्षा में ऐसी त्रुटि का रह जाना संभव है, किन्तु ईश्वरीय क़ानून इतना दोषपूर्ण (होना तो दूर की बात, तनिक भी दोषपूर्ण) नहीं हो सकता। उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मानव-रक्त की प्रतिष्ठा केवल उसी समय तक है, जब तक उस पर ‘हक़’ (सत्य और न्याय) न क़ायम हो जाए। (जब तक कि वह अपराध करके स्वयं उस प्रतिष्ठा को भंग न कर दे।) उसे जीवन का अधिकार केवल वैध सीमाओं के भीतर ही दिया जा सकता है, किन्तु जब वह उन सीमाओं का उल्लंघन करके उपद्रव और फ़साद फैलाए या दूसरों के जान पर आक्रमण करे तो वह अपने जीवन-अधिकार को स्वयं खो देता है और उसका वध वैध हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु ही मानवता का जीवन हो जाती है। अतएव कहा गया है कि, ‘‘हत्या बड़ी बुरी चीज़ है किन्तु उससे अधिक बुरी चीज़ फ़साद एवं उपद्रव है।’’ जब कोई व्यक्ति यह बड़ा अपराध करे तो उसकी बड़ी बुराई का अंत कर देना ही ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार जो कोई किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति की अन्यायपूर्ण हत्या करे, उसके लिए आदेश हुआ ‘‘ मारे जाने वालों के विषय में हत्या-दंड (क़िसास) तुम पर अनिवार्य किया गया’’ (कु़रआन, 2:178)। इसके साथ उस भेदभाव को भी मिटा दिया गया जिसे गुमराह क़ौमों ने उच्च और निम्न वर्ग के लोगों में क़ायम किया था। अतएव कहा गया ‘‘हमने उस (तौरात) में उनके लिए लिख दिया था कि जान जान के बराबर है’’ (क़ुरआन, 5:45)। यह नहीं हो सकता कि अमीर ग़रीब को मार डाले या आज़ाद व्यक्ति ग़ुलाम की हत्या कर दे तो वह छोड़ दिया जाए, बल्कि मनुष्य होने की दृष्टि से सब बराबर हैं। जान के बदले जान ही लिया जाएगा, चाहे धनी का जान हो या निर्धन का। फिर इस विचार से कि किसी को इस अवश्यम्भावी रक्तपात में झिझक न हो, कहा गया, ‘‘ऐ बुद्धिमानो! तुम्हारे लिए जान-दंड में जीवन है।’’ (2:179); अर्थात् ऐ बुद्धिमानो! इस जान-दंड को मृत्यु न समझो, बल्कि यह तो वास्तव में समाज का जीवन है जो उसके शरीर से एक दूषित और घातक फोड़े को काटकर प्राप्त किया जाता है। जान-दंड से प्राप्त होने वाले जीवन के इस दर्शन को पैग़म्बर (सल्ल॰) ने एक अवसर पर भली-भाँति समझाया है। आप (सल्ल॰) ने कहा, ‘‘अपने भाई की सहायता करो, चाहे वह अत्याचारी हो या अत्याचार-पीड़ित।’’ सुनने वाले को आश्चर्य हुआ कि अत्याचार-पीड़ित की सहायता तो उचित है, किन्तु अत्याचारी की यह सहायता कैसी? पूछा, ‘‘ऐ ईशदूत! हम अत्याचार-पीड़ित की सहायता तो अवश्य करेंगे, किन्तु अत्याचारी की सहायता किस तरह करें?’’ आप (सल्ल॰) ने कहा, ‘‘इस तरह कि तू उसका हाथ पकड़ ले और उसे अत्याचार करने से रोक दे।’’ अतः वस्तुतः ज़ालिम के जु़ल्म को रोकने में उसके साथ जो सख़्ती भी की जाए, वह सख़्ती नहीं है, बल्कि वह नर्मी ही है और स्वयं उस अत्याचारी की भी सहायता ही है। इसीलिए इस्लाम में ईश्वरीय हद को क़ायम करने (ईश्वर की ओर से निर्धारित दंडों को व्यवहार में लाने) की सख़्ती के साथ ताकीद की गई है और इसे दयालुता और उसके प्रसाद का कारण बताया गया है। ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा है, ‘‘ईश्वर की हदों में से एक हद क़ायम करने की बरकत चालीस दिन की वर्षा से अधिक है।’’ वर्षा की बरकत यह है कि इससे धरती सिंचित होती है, फ़सलें भली-भाँति तैयार होती हैं, ख़ुशहाली में वृद्धि होती है। किन्तु हद के क़ायम करने (अर्थात दंड-विधान को लागू करने) की बरकत और लाभ इससे बढ़कर है क्योंकि इससे उपद्रव, बिगाड़, अत्याचार और अशान्ति का उन्मूलन होता है, ईश्वर के पैदा किए हुए प्राणियों को शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है और शान्ति-स्थापना से वह परितोष उपलब्ध होता है जो सामाजिकता की आत्मा और उन्नति का जान है।
सत्य एवं न्याय को ‘अपेक्षित’ और ‘अनपेक्षित’ हत्या में अन्तर
सत्य और न्याय के अनपेक्षित क़त्ल को ऐसी कड़ाई के साथ रोककर और सत्य और न्याय को अपेक्षित क़त्ल की ऐसी ताकीद करके ईश्वरीय धर्म-विधान ने अतिशयता और न्यूनता के दो मार्गों के मध्य न्याय और बीच के सीधे मार्ग की ओर हमारा मार्गदर्शन किया है। एक ओर वह मर्यादाहीन और सीमोल्लंघन करने वाला गिरोह है जो मानव-जान का कोई मूल्य नहीं समझता और अपनी तुच्छ इच्छाओं पर उसे बलिदान कर देना वैध समझता है। दूसरी ओर वह विवेकभ्रष्ट और दृष्टिभ्रष्ट गिरोह है जो रक्त की पवित्रता और उसकी शाश्वत अवैधता का मानने वाला है और किसी स्थिति में भी रक्त बहाना वैध नहीं समझता। इस्लामी धर्म-विधान ने इन दोनों ग़लत विचारों का खंडन कर दिया और उसने बताया कि मानव-जान की प्रतिष्ठा न तो काबा या माँ-बहन की प्रतिष्ठा की तरह शाश्वत है कि किसी प्रकार उसे क़त्ल करना वैध ही न हो सके और न उसका मूल्य इतना कम है कि अपनी तुच्छ भावनाओं एवं इच्छाओं की तृप्ति के लिए उसका वध कर देना वैध हो। एक ओर उसने बताया कि मानव-जान इसलिए नहीं है कि मनोरंजन के लिए घातक दशा में उसके तड़पने का तमाशा देखा जाए, उसको जलाकर या यातनाएँ देकर आनन्द लिया जाए, उसको व्यक्तिगत इच्छाओं की राह में रुकावट समझकर उसका अन्त कर दिया जाए या तथ्यहीन अंधविश्वासों और ग़लत रीतियों की वेदी पर उसकी भेंट चढ़ाई जाए। ऐसे अपवित्रा उद्देश्यों के लिए उसका ख़ून बहाना निश्चय ही अवैध और महापाप है। दूसरी ओर उसने यह भी बताया कि एक चीज़ मानव-जान से भी अधिक मूल्यवान है और वह ‘हक़’ (सत्य एवं न्याय) है। वह जब उसके ख़ून की माँग करे तो उसे बहाना न केवल वैध बल्कि अनिवार्य है और उसको न बहाना सबसे बड़ा गुनाह है। मनुष्य जब तक सत्य का आदर करता है उसके ख़ून का आदर करना आवश्यक होता है, किन्तु जब वह उद्दंड होकर सत्य पर हाथ बढ़ाए तो वह अपने ख़ून का मूल्य स्वयं खो देता है। फिर उसके ख़ून का मूल्य इतना भी नहीं रहता, जितना पानी का होता है।
अवश्यम्भावी रक्तपात
सत्य और न्याय को अपेक्षित क़त्ल यद्यपि देखने में सत्य के अनपेक्षित क़त्ल की तरह रक्तपात ही है, किन्तु वास्तव में यह अवश्यम्भावी रक्तपात है जिससे किसी दशा में छुटकारा नहीं। इसके बिना न संसार में शान्ति स्थापित हो सकती है, न बुराई और फ़साद की जड़ कट सकती है, न नेक लोगों को बुरों की दुष्टता से मुक्ति मिल सकती है, न हक़दार को हक़ मिल सकता है, न ईमानदारों को ईमान और अन्तरात्मा की स्वतंत्राता प्राप्त हो सकती है, न उद्दंडों को उनकी वैध सीमाओं में सीमित रखा जा सकता है और न ईश्वर के प्राणियों को भौतिक एवं आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हो सकती है। यदि इस्लाम पर ऐसे रक्तपात का आरोप है तो उसे इस आरोप को स्वीकार करने में तनिक भी लज्जा नहीं। किन्तु (यदि ऐसे रक्तपात को निन्दनीय मान भी लिया जाए तो) प्रश्न यह है कि फिर और कौन है जिसका दामन इस अवश्यम्भावी रक्तपात के छींटों से रंजित नहीं है? बौद्धमत की अहिंसा इसको वैध ठहराती है, किन्तु वह भी भिक्षु और गृहस्थ में अन्तर करने पर विवश हुई और अंततः उसने एक छोटे गिरोह के लिए मुक्ति (निर्वाण) को आरक्षित रखने के पश्चात् शेष सम्पूर्ण संसार को कुछ नैतिक आदेश देकर गृहस्थधर्म स्वीकार करने के लिए छोड़ दिया, जिसमें राजनीति, दंड-विधान और युद्ध सब कुछ है। इसी प्रकार ईसाइयत भी युद्ध को सर्वथा अवैध ठहराने के बावजूद अन्ततः युद्ध के लिए विवश हुई और जब रोम साम्राज्य के अत्याचारों को सहन करना उसके लिए असंभव हो गया तो अन्ततः उसने स्वयं राज्य पर क़ब्ज़ा करके ऐसा युद्ध छेड़ा जो अवश्यम्भावी रक्तपात की सीमा से बहुत आगे निकल गया। हिन्दू धर्म में भी अर्वाचीन दार्शनिकों ने ‘अहिंसा परमो धर्मः’ की धारणा प्रस्तावित की और जीव-हत्या को पाप ठहराया। किन्तु जब इस संबंध में क़ानूनविद् मनु से धर्मादेश (फ़तवा) मालूम किया गया कि ‘‘यदि कोई व्यक्ति हमारी स्त्रियों पर हाथ डाले या हमारा धन छीने, हमारे धर्म का अपमान करे तो हम क्या करें?’’ तो उसने उत्तर दिया कि ‘‘ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को अवश्य मार डालना चाहिए, भले ही वह गुरु हो या विद्वान ब्राह्मण, बूढ़ा हो या नवयुवक।’’
(गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं व बहुश्रुतम्।
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्।। (मनु 8/350)
‘‘गुरु, बालक, वृद्ध या बहुत शास्त्रों का जानने वाला ब्राह्मण भी आततायी होकर आए तो उसे बेखटके मार डाले।’’)
यहाँ धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके इस अवश्यम्भावी रक्तपात की आवश्यकता सिद्ध करने का अवसर नहीं है। धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन एक अलग चीज़ है जिसे यथावसर प्रस्तुत किया जाएगा और उस समय यह सिद्ध हो जाएगा कि जो धर्म युद्ध को बुरा समझते हैं, वे भी व्यावहारिक जगत् में पदार्पण के पश्चात् इस अवश्यम्भावी चीज़ से अपने आपको अलग रखने में असमर्थ रहे हैं। इस समय हमारा उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि नैतिक प्रदर्शन के लिए कोई गिरोह चाहे कैसे ही ऊँचे काल्पनिक दर्शनों तक पहुँच जाए, किन्तु व्यावहारिक जगत में आकर उसे संसार की तमाम समस्याओं को व्यवहारतः हल करना पड़ता है और यह संसार स्वयं उसको विवश कर देता है कि वह उसके यथार्थ का व्यावहारिक उपायों से मुक़ाबला करे। कु़रआन अवतरित करने वाले (ईश्वर) के लिए यह कुछ कठिन कार्य न था कि वह जान-सम्मान के लिए उसी प्रकार के काल्पनिक, आनन्ददायक नियम प्रस्तुत करता, जैसे कि अहिंसा की धारणा में पाए जाते हैं और निश्चय ही वह अपनी चामत्कारिक वाणी में उनको प्रस्तुत करके संसार को आश्चर्यचकित कर सकता था। किन्तु उस जगत्-स्रष्टा को भाषण और दार्शनिकता का प्रदर्शन अभीष्ट न था, बल्कि वह अपने बन्दों के लिए एक सत्यानुवू$ल और स्पष्ट व्यवहार-संहिता प्रस्तुत करना चाहता था, जिसका पालन करके उनका लोक और धर्म दोनों सँवर सके। इसलिए जब उसने देखा कि ‘‘यह और बात है कि सत्य और न्याय को (क़त्ल) अपेक्षित हो’’ के अपवाद के बिना, मात्रा ‘जीव-हत्या न करो’ का सामान्य आदेश लाभदायक नहीं हो सकता तो यह उसकी अवगुणरहित सत्ता के प्रतिवू$ल था कि दुनिया वालों को ‘‘तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो’’ (क़ुरआन, 61:3), का ताना देने के बावजूद वह उन्हें यह सिखाता कि ज़बान से ‘अहिंसा परमो धर्मः’ की आवाज़ बुलन्द करो और हाथ से ख़ूब तलवार चलाते रहो। अतः यह ईश्वर की पूर्ण तत्वदर्शिता ही थी कि उसने जान-सम्मान की शिक्षा के साथ जान-दंड का क़ानून भी निर्धारित किया और इस तरह उस शक्ति को प्रयुक्त करने को आवश्यक ठहराया जिसका प्रयोग जान-प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अवश्यम्भावी है।
सामूहिक उपद्रव
यह जान-दंड का क़ानून जिस प्रकार व्यक्तियों के लिए है उसी प्रकार समूहों के लिए भी है। जिस प्रकार व्यक्ति उद्दंड होते हैं, उसी प्रकार गिरोह और क़ौमें भी उद्दंड होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति लालच और लोलुपता से अभिभूत होकर सीमोल्लंघन कर जाते हैं, उसी प्रकार गिरोह और क़ौमों में भी यह नैतिक रोग पैदा हो जाया करता है। अतः जिस प्रकार व्यक्तियों को क़ाबू में रखने और उन्हंे अत्याचार से रोकने के लिए युद्ध अवश्यम्भावी हो जाता है उसी प्रकार गिरोहों और क़ौमों के बढ़ते हुए दुष्कर्मों को रोकने के लिए भी युद्ध अवश्यम्भावी हो जाता है। आकार-प्रकार की दृष्टि से व्यक्तिगत और सामूहिक उपद्रव में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु प्रकृति की दृष्टि से बहुत बड़ा अन्तर है। व्यक्तियों के उपद्रव का क्षेत्रा अत्यंत सीमित होता है, मनुष्यों के एक छोटे समूह को उससे कष्ट पहुँचता है और गज़ भर धरती रक्त-रंजित करके उसका उन्मूलन किया जा सकता है। किन्तु गिरोहों का उपद्रव एक असीम संकट होता है जिससे अनगिनत मनुष्यों की ज़िन्दगी दूभर हो जाती है, पूरी-पूरी क़ौमों का जीवन संकीर्ण होकर रह जाता है। सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एक हलचल पैदा हो जाता है और उसका उन्मूलन ख़ून की नदियाँ बहाए बिना नहीं हो सकता, जिसे कुरआन में ‘धरती में रक्तपात’ (कु़रआन, 8:67) के अर्थयुक्त शब्द से अभिव्यंजित किया गया है।
गिरोह जब उद्दंडता पर उतर आते हैं तो वे कोई एक उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनमें तरह-तरह के शैतान सम्मिलित होते हैं इसलिए तरह-तरह की शैतानी ताक़तें उनके तूफ़ान में उभर आती हैं और हज़ारों प्रकार के उपद्रव उनके कारण उठ खड़े होते हैं। कुछ उनमें धन-दौलत के लालची होते हैं तो वे ग़रीब क़ौमों पर डाके डालते हैं, उनके व्यापार पर क़ब्ज़ा करते हैं, उनके उद्योगों को नष्ट करते हैं, उनके परिश्रम से कमाए हुए धन को विभिन्न प्रकार की चालाकियों से लूटते हैं और ताक़त के बल पर उस धन से अपने कोष भरते हैं जिसके वैध अधिकारी वे भूखी, पीड़ित क़ौमें होती हैं। कुछ उनमें अपनी तुच्छ इच्छाओं के दास होते हैं। वे अपने जैसे लोगों को ख़ुदा बन बैठते हैं, अपनी इच्छाओं पर निर्बलों के अधिकारों की बलि चढ़ाते हैं। न्याय को मिटाकर अन्याय और अत्याचार के झंडे बुलन्द करते हैं। सज्जनों और नेक लोगों को दबाकर मूर्खों और कमीनों को ऊँचा उठाते हैं, उनके अपवित्र प्रभाव से क़ौमों के नैतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, सद्गुणों और श्रेष्ठताओं के स्रोत सूख जाते हैं और उनकी जगह विश्वासघात, दुष्कर्म, अश्लीलता, कठोर हृदयता, अन्याय और अनगिनत अन्य नैतिक दुर्गुणों के गन्दे नाले जारी हो जाते हैं। फिर उनमें कुछ वे होते हैं जिन पर देश एवं विश्व-विजय का भूत सवार होता है वे निरुपाय और निर्बल क़ौमों की आज़ादियाँ छीन लेते हैं। ख़ुदा के बेगुनाह बन्दों के ख़ून बहाते हैं, अपनी सत्तालोलुपता को पूरा करने के लिए धरती में फ़साद फैलाते हैं और स्वतंत्र लोगों को उस गु़लामी का तौक़ पहनाते हैं जो समस्त नैतिक बिगाड़ की जड़ है। इन शैतानी कामों के साथ जब धर्म में ज़ोर-ज़बरदस्ती भी शामिल हो जाती है और इन अत्याचारी गिरोहों में से कोई गिरोह अपने स्वार्थों के लिए धर्म को प्रयोग करके ख़ुदा के बन्दों को धार्मिक स्वतंत्रता से भी वंचित कर देता है और दूसरों पर इसलिए अत्याचार करता है कि वे उसके धर्म के बजाय अपने धर्म का पालन क्यों करते हैं, तो यह संकट और भी गंभीर हो जाता है।
युद्ध : एक नैतिक कर्तव्य
ऐसी स्थिति में युद्ध वैध ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। उस समय मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि उन ज़ालिमों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उन फ़सादियों और उपद्रवियों की बुराई से ईश्वर के पीड़ित एवं निरुपाय बन्दों को छुटकारा दिलाया जाए जो शैतान बनकर आदम की संतान पर नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विनाश का संकट लाते हैं। वे लोग वास्तव में मनुष्य नहीं होते कि मानवीय सहानुभूति के हक़दार हों, बल्कि मनुष्य के भेष में शैतान और मानवता के वास्तविक शत्रु होते हैं, जिनके साथ वास्तविक सहानुभूति यही है कि उनकी बुराई को विश्व-पटल से अशुद्ध अक्षर की तरह मिटा दिया जाए। वे अपनी करतूतों से अपने जीवन-अधिकार को स्वयं खो देते हैं। उन्हें और उन लोगों को, जो उनकी बुराई को बाक़ी रखने के लिए उनकी सहायता करें, संसार में जीवित रहने का अधिकार शेष नहीं रहता। वे वास्तव में मानव-शरीर का ऐसा अंग होते हैं जिसमें विषाक्त और विकृत तत्व भर गया हो, जिसके बाक़ी रहने से सम्पूर्ण शरीर के विनष्ट हो जाने की आशंका हो। इसलिए बुद्धि और निहित हितदर्शिता की अपेक्षा यही है कि उस विकृत और घातक अंग को काट पें$का जाए। बहुत संभव है कि संसार में कोई कल्पना-लोक में विचरने वाला शिक्षक (या शिक्षार्थी) ऐसा भी हो जिसकी दृष्टि में ऐसे ज़ालिमों का क़त्ल भी पाप हो और उसकी कायर आत्मा उस रक्त के प्लावन की कल्पना से काँप उठती हो जो उनकी बुराई के उन्मूलन में बहती है। किन्तु ऐसा शिक्षक संसार का सुधार नहीं कर सकता। वह जंगलों और पहाड़ों में जाकर आत्मसंयम और तपस्या से अपनी आत्मा को तो अवश्य शान्ति पहुँचा सकता है, किन्तु उसकी शिक्षा दुनिया को बुराई से पाक करने और अत्याचार और उद्दंडता से सुरक्षित रखने में कभी सफल नहीं हो सकती। वह आत्म-दमन करने वाले मनुष्यों का एक ऐसा गिरोह तो अवश्य जुटा सकता है जो उत्पीड़ितों के साथ अत्याचार सहने में स्वयं भी सम्मिलित हो जाए, किन्तु उच्च साहस वाले मनुष्यों का ऐसा गिरोह पैदा करना उसके वश की बात नहीं है जो जु़ल्म को मिटाकर न्याय स्थापित कर दे और ईश्वर के पैदा किए हुए प्राणियों के लिए शान्तिपूर्वक रहने और मानवता के उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के साधन जुटा दे।
व्यावहारिक नैतिकता, जिसका उद्देश्य सामाजिकता की समुचित व्यवस्था स्थापित करना है, वास्तव में एक दूसरा ही दर्शन है जिसमें काल्पनिक आनन्द की सामग्री ढूंढ़ना व्यर्थ है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र का उद्देश्य कामवासना और भोज्य पदार्थ का सुख-स्वाद नहीं, बल्कि शरीर का सुधार है, चाहे कड़वी दवा से हो या मीठी से, उसी प्रकार नैतिकता का उद्देश्य भी अभिरुचि एवं दृष्टि का आनन्द नहीं है, बल्कि संसार का सुधार है, चाहे कड़ाई से हो या नर्मी से। कोई सच्चा नैतिक सुधारक तलवार और क़लम में से केवल एक ही चीज़ को अपनाने और एक ही साधन से सुधार का कर्तव्य निभाने की क़सम नहीं खा सकता, उसको अपना पूरा काम करने के लिए दोनों चीज़ों की समान रूप से आवश्यकता है। जब तक उपदेश और प्रचार उन्मादी गिरोहों को नैतिकता एवं मानवता की मर्यादाओं का पाबन्द बनाने में सफल हो सकता हो, उनके विरुद्ध तलवार उठाना अवैध बल्कि हराम है, मगर जब किसी गिरोह की शरारत और दुष्प्रकृति इस हद तक बढ़ गई हो कि उसे उपदेश और शिक्षा द्वारा रास्ते पर न लाया जा सके और जब उसको दूसरों पर हाथ डालने, दूसरों के अधिकार छीनने, दूसरों की इज़्ज़त और बड़ाई पर हमला करने से और दूसरों के नैतिक एवं आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को नष्ट करने से रोकने के लिए युद्ध के सिवा कोई उपाय शेष न रहे तो फिर यह मानव के प्रत्येक हितैषी का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि उसके विरुद्ध तलवार उठाए और उस समय तक चैन न ले जब तक ईश-सृष्ट प्राणियों को उनके खोए अधिकार वापस न मिल जाएँ।
युद्ध का निहित उद्देश्य
युद्ध के इसी निहित उद्देश्य और आवश्यकता को तत्वदर्शी और सर्वज्ञ ईश्वर ने अपनी ज्ञान-गर्भित वाणी में इस प्रकार व्यक्त किया है:
‘‘यदि ईश्वर लोगों को एक-दूसरे के द्वारा हटाता न रहता तो मठ और गिरजा और यहूदी उपासनागृह और मस्जिदें, जिनमें ईश्वर का अधिक नाम लिया जाता है, सब ढा दी जातीं।’’ (क़ुरआन, 22:40)
क़ुरआन की इस शुभ आयत में केवल मुसलमानों की मस्जिदों का ही उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि ‘सवामेअ़’ ‘बिअ़’ और ‘सलवात’ तीन और चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। ‘सवामेअ़’ से अभिप्रेत ईसाइयों के संन्यासी गृह, मजूसियों के पूजागृह और साबियों के उपासना-ग्रह हैं। ‘बिअ़’ के शब्द में ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के कलीसे दोनों सम्मिलित हैं। यह सारगर्भित शब्द प्रयोग करने के पश्चात् फिर ‘सलवात’ का एक ऐसा शब्द प्रयोग किया है जो व्यापकता किए हुए हैं, जो ईश्वरीय आराधना के प्रत्येक विषय का द्योतक है। और इन सबके अंत में मस्जिदों का उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्रेत यह बताना है कि अगर ईश्वर न्यायप्रिय मनुष्यों के द्वारा अत्याचारी लोगों को न हटाया करता तो इतना बड़ा बिगाड़ पैदा होता कि उपासना-गृह तक बर्बादी से न बचते जिनसे नुक़सान की किसी को आशंका नहीं हो सकती। इसके साथ ही यह भी बता दिया कि बिगाड़ का सबसे घृणित रूप यह है कि एक जाति शत्रुता से प्रेरित होकर दूसरी जाति के उपासना-ग्रहों तक को नष्ट कर दे। और फिर अत्यंत प्रभावकारी ढंग से अपने इस अभिप्राय को भी व्यक्त कर दिया कि जब कोई गिरोह ऐसा बिगाड़ पैदा करता है तो हम किसी दूसरे गिरोह के द्वारा उसकी दुष्टता का उन्मूलन कर देना आवश्यक समझते हैं।
युद्ध के इसी निहित उद्देश्य को दूसरे स्थान पर जालूत की सरकशी और हज़रत दाऊद (अलैहि॰) के हाथ से उसके मारे जाने का उल्लेख करते हुए इस प्रकार कहा है:
‘‘यदि ईश्वर मनुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती बिगाड़ से भर जाती, किन्तु ईश्वर संसार वालों के लिए उदार अनुग्राही है (कि वह बिगाड़ को दूर करने का यह प्रबंध करता रहता है)।’’ (क़ुरआन, 2:251)
एक और जगह क़ौमों की पारस्परिक शत्रुता और वैर का उल्लेख करके कहा जाता है:
‘‘वे जब भी युद्ध की आग भड़काते हैं, ईश्वर उसको बुझा देता है। वे धरती में बिगाड़ फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हालाँकि ईश्वर बिगाड़ फैलाने वालों को पसन्द नहीं करता।’’ (क़ुरआन, 5:64)
ईश्वरीय मार्ग में युद्ध (जिहाद) की आवश्यकता
यहाँ इसी बिगाड़ और अशान्ति, लालच और लोलुपता, द्वेष और शत्रुता और पक्षपात और संकीर्ण दृष्टता का युद्ध है जिसकी आग को बुझाने के लिए ईश्वर ने अपने नेक बन्दों को तलवार उठाने (अर्थात् शक्ति प्रयोग) का आदेश दिया है। अतएव कहा गया:
‘‘जिन लोगों से युद्ध किया जा रहा है उन्हें लड़ने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि उन पर जु़ल्म हुआ है। और निश्चय ही ईश्वर उनकी सहायता की पूरी सामथ्र्य रखता है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से बेकु़सूर निकाले गए, इनका कु़सूर केवल यह था कि ये ईश्वर को अपना पालनहार कहते थे।’’ (क़ुरआन, 22:39-40)
यह क़ुरआन में पहली आयत है जो युद्ध के संबंध में उतरी। इसमें जिन लोगों के विरुद्ध लड़ने का आदेश दिया गया है, उनका दोष यह नहीं बताया कि उनके पास एक उपजाऊ भूमि है या वे व्यापार की एक बड़ी मंडी के मालिक हैं या वे एक अन्य धर्म का पालन करते हैं, बल्कि उनका अपराध स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वे अत्याचार करते हैं, निर्दोष लोगों को उनके घरों से निकालते हैं और पक्षपात में इतने अधिक ग्रस्त हैं कि लोगों को केवल इसलिए दुख देते हैं और उन्हें संकट में डालते हैं कि वे लोग ईश्वर को अपना पालनहार कहते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध केवल अपनी ही सुरक्षा हेतु युद्ध का आदेश नहीं दिया गया, बल्कि दूसरे उत्पीड़ित लोगों की सहायता और उनके समर्थन का भी आदेश दिया गया है और ताकीद की गई है कि कमज़ोर और निस्सहाय लोगों को ज़ालिमों के पंजे से छुड़ाओ:
‘‘तुम्हें क्या हो गया है कि ईश्वर के मार्ग में उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध नहीं करते, जो प्रार्थनाएँ करते हैं कि हमारे प्रभु! तू हमें उस बस्ती से निकाल जहाँ के लोग बड़े ज़ालिम और दमनकारी हैं, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई सहायक और समर्थक नियुक्त कर।’’ (क़ुरआन, 4:75)
ऐसे युद्ध को, जो ज़ालिमों और फ़सादियों के मुक़ाबले में अपनी सुरक्षा और कमज़ोरों, असहायों और उत्पीड़ितों की सहायता के लिए किया जाए, ईश्वर ने उसे ठीक ‘ईश्वरीय मार्ग का युद्ध’ ठहराया है, जिससे यह बताना अभीष्ट है कि यह युद्ध बन्दों के लिए नहीं, बल्कि ख़ुदा के लिए है और बन्दों के स्वार्थ और उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रसन्नता के लिए है। इस युद्ध को उस समय तक जारी रखने का आदेश दिया गया है जब तक ईश्वर के निर्दोष बन्दों पर ज़ालिमों का अपनी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाथ डालने और दमन और अत्याचार का सिलसिला बन्द न हो जाए। अतएव कहा गया, ‘‘उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि उपद्रव शेष न रहे।’’ (क़ुरआन, 2:193); और ‘‘यहाँ तक कि युद्ध अपने हथियार डाल दे और बिगाड़ का नामो-निशान इस तरह मिट जाए कि उसके मुक़ाबले के लिए युद्ध की आवश्यकता न रहे।’’ (क़ुरआन, 47:4); इसके साथ यह भी बता दिया है कि सत्य पर आधारित इस युद्ध को रक्तपात समझकर छोड़ देने या उसमें जान और धन की हानि देखकर संकोच करने का परिणाम कितना बुरा है।
सत्य-असत्य का सीमा-निर्धारण
फिर ईश्वर ने सत्य-समर्थन के युद्ध के निहित उद्देश्य और आवश्यकता को व्यक्त करने और ताकीद करने ही पर बस नहीं किया, बल्कि यह स्पष्टीकरण भी कर दिया कि:
‘‘जो लोग ईमान वाले हैं वे ईश्वर के मार्ग में युद्ध करते हैं और जो इन्कार करने वाले और अवज्ञाकारी हैं वे अत्याचार और उद्दंडता के लिए लड़ते हैं। अतः तुम शैतान के मित्रों से लड़ो। क्योंकि शैतान की लड़ाई का पहलू कमज़ोर है।’’
(क़ुरआन, 4:76)
यह एक निर्णायक कथन है जिसमें सत्य और असत्य के मध्य पूर्ण रूप से सीमा-निर्धारण कर दिया गया है। जो लोग जु़ल्म और सरकशी के लिए युद्ध करें वे शैतान के मित्रा हैं और जो जु़ल्म के लिए नहीं, बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए युद्ध करें वे ईश्वरीय मार्ग के धर्मयोद्धा (मुजाहिद) हैं। प्रत्येक वह युद्ध जिनका उद्देश्य सत्य एवं न्याय के विरुद्ध ईश्वर के बन्दों को तकलीफ़ देना हो, जिसका उद्देश्य हक़दारों का हक़ छीनना और उन्हें उनकी वैध सम्पत्तियों से निष्कासित करना हो, जिसका उद्देश्य ईश्वर का नाम लेने वालों को अकारण सताना हो, वह युद्ध शैतान के मार्ग में है। उसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं। ऐसा युद्ध करना ईमान वालों का काम नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसे ज़ालिमों के मुक़ाबले में उत्पीड़ितों का समर्थन और उनकी रक्षा करते हैं, जो संसार से अन्याय एवं अत्याचार को मिटाकर न्याय स्थापित करना चाहते हैं, जो सरकशों और फ़सादियों की जड़ काटकर ख़ुदा के बन्दों को निश्चिन्तता और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने और मानवता के उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का अवसर देते हैं, उनका युद्ध ईश्वरीय मार्ग का युद्ध है। वे उत्पीड़ितों की जो सहायता करते हैं तो मानो वे स्वयं ईश्वर की सहायता करते हैं, और ईश्वर ने उन्हीं की सहायता का वचन दिया है।
ईश्वर के मार्ग में जिहाद की विशिष्टता
यही वह ईश्वरीय मार्ग का जिहाद है जिसकी विशिष्टता के वर्णन से क़ुरआन के पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिसके विषय में कहा है:
‘‘ऐ ईमान वालो क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊँ जो तुम्हें पीड़ाजनक यातना से बचाए। वह तिजारत यह है कि तुम ईश्वर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में अपनी जान-माल से जिहाद करो। यह तुम्हारे लिए उत्तम कार्य है यदि तुम जानो।’’ (क़ुरआन, 61:10-11)
जिसमें लड़ने वालों की प्रशंसा इस तरह की है:
‘‘ईश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो उसके मार्ग में इस तरह पंक्तिबद्ध होकर लड़ते हैं मानो वे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं।’’ (क़ुरआन, 61:4)
जिसकी उच्चता एवं महानता की गवाही इस शान से दी है:
‘‘क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और प्रतिष्ठित मस्जिद (काबा) के आबाद करने को उन लोगों के काम के बराबर ठहराया है जो ईश्वर और अन्तिम दिन पर ईमान लाए और ईश्वर के मार्ग में लड़े? ईश्वर की दृष्टि में ये दोनों बराबर नहीं हैं। ईश्वर ज़ालिम लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने सत्य के लिए घरबार छोड़े और ईश्वरीय मार्ग में जान-माल से लड़े उनका दर्जा ईश्वर की दृष्टि में ज़्यादा बड़ा है, और वही लोग हैं जो वास्तव में सफल हैं।’’ (क़ुरआन, 9:19-20)
फिर यही वह सत्यप्रियता का युद्ध है जिसमें एक रात का जागना हज़ार रातें जागकर उपासना करने से बढ़कर है, जिसके क्षेत्रा में जमकर खड़े होने, घर बैठकर साठ वर्ष तक नमाज़ें पढ़ते रहने से उत्तम बताया गया है, जिसमें जागने वाली आंख पर नरक की आग हराम कर दी गई है, जिसके मार्ग में धूल-धूसरित होने वाले क़दमों से वादा किया गया है कि वे कभी नरकाग्नि की ओर न घसीटे जाएँगे ओर इसके साथ ही उन लोगों को जो उससे बचकर घर बैठ जाएँ और उसकी पुकार सुनकर कसमसाने लगें, इस प्रकोपयुक्त शैली में सचेत किया गया है:
‘‘उनसे कह दो यदि तुम्हें अपने पिता, बेटे, भाई, पत्नियाँ, नातेदार और वे धन जो तुमने कमाए हैं और वह तिजारत जिसके मंद पड़ जाने का तुम्हें भय लगा हुआ है और वे घर-बार जिन्हें तुम पसन्द करते हो, ईश्वर और उसके रसूल और उसके मार्ग में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं तो बैठे प्रतीक्षा करते रहो, यहाँ तक कि ईश्वर अपना काम पूरा करे। विश्वास रखो कि ईश्वर अवज्ञाकारियों का कभी मार्गदर्शन नहीं करता।’’ (क़ुरआन, 9:24)
युद्ध की महत्ता का कारण
विचार कीजिए कि ईश्वरीय मार्ग में जिहाद की इतनी महत्ता और प्रशंसा किस लिए है? जिहाद करने वालों को बार-बार क्यों कहा जाता है कि वही सफल हैं और उन्हीं का दर्जा ऊँचा है? और उससे बचकर घर बैठने वालों को ऐसी चेतावनियाँ क्यों दी जाती हैं? इस सवाल को हल करने के लिए तनिक क़ुरआन की उन आयतों पर फिर एक दृष्टि डाल लीजिए जिनमें जिहाद का आदेश और उसका महत्व और विशिष्टता और उससे भागने की बुराई बयान की गई है। इन आयतों में सफलता और महानता का अर्थ किसी स्थान पर भी धन-दौलत और देश और राज्य का प्राप्त करना नहीं बताया गया। कु़रआन में कहीं यह कहकर ईश्वरीय मार्ग में लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है कि इसके बदले तुम्हें सांसारिक धन और राज्य प्राप्त होगा। बल्कि इसके विपरीत प्रत्येक जगह ईश्वरीय मार्ग में जिहाद के बदले ईश-प्रसन्नता और केवल ईश्वर के यहाँ बड़ा दर्जा मिलने और पीड़ादायी यातना से सुरक्षित रहने की आशा दिलाई गई है। हाजियों को पानी पिलाना और प्रतिष्ठित मस्जिद (काबा) के आबाद करने से जो, अरब में बड़ी पहुँच और प्रभाव और बड़ी आमदनी का साधन था, घरबार छोड़कर निकल जाने और ईश्वरीय मार्ग में जिहाद करने को श्रेष्ठ काम बताया और फिर इसके बदले ‘‘ईश्वर के निकट बड़े दर्जे’’ के सिवा और किसी पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया। दूसरी जगह एक व्यापार का गुर सिखाया है जिससे ख़्याल होता है कि शायद यहाँ कुछ धन-दौलत का उल्लेख हो। किन्तु पढ़कर देखिए तो इस व्यापार की वास्तविकता यह निकलती है कि ईश्वर के मार्ग में जान और माल खपाओ और इसके बदले में यातना से छुटकारा प्राप्त करो। एक और स्थान पर लड़ाई से जी चुराने वालों को इस बात पर डाँटा जा रहा है कि वे बीवी-बच्चों के प्रेम में ग्रस्त पाए जाते हैं और अपने कमाए हुए धन अपने व्यापार की मन्दी और अपने मनभाते घरों के छूटने से डरते हुए दिखाई देते हैं। जब कि दुनिया में युद्ध करके जो लोग देश पर विजय प्राप्त करते हैं उन्हें रुपया भी ख़ूब मिलता है, उनका व्यापार भी ख़ूब चमकता है और उन्हें विजित जाति से छीने हुए भव्य भवन भी रहने को मिलते हैं।
फिर जब इस जिहाद से सांसारिक धन और देश पर विजय पाना अभीष्ट नहीं है तो फिर इस रक्तपात से ईश्वर को क्या मिलता है कि वह इसके बदले में इतने बड़े-बड़े दर्जे दे रहा है? फिर इस आशंकापूर्ण काम में क्या रखा है जिसकी भाग-दौड़ से धूल-धूसरित पैरों तक को कृपा-दृष्टि और अनुकम्पा का कारण बताया जाता है और फिर इसमें कौन-सी सफलता निहित है कि इस शुष्क और निस्वाद युद्ध में लड़ने वालों को बारम्बार ‘‘वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं’’ कहा जा रहा है? इसका उत्तर ‘‘और यदि ईश्वर मनुष्यों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती बिगाड़ से भर जाती’’, ‘‘अगर तुम यह न करोगे तो धरती में फ़ित्ना (उपद्रव) और बड़ा बिगाड़ पैदा होगा’’ में निहित है। ईश्वर यह नहीं चाहता कि उसकी धरती पर उपद्रव और बिगाड़ फैलाया जाए। वह यह सहन नहीं कर सकता कि उसके बन्दों को अकारण सताया और तबाह और बर्बाद किया जाए। उसे यह पसन्द नहीं है कि बलवान दुर्बलों को खा जाएँ, उनकी शान्ति पर डाके डालें और उनके नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को तबाही में डाल दें। उसे यह स्वीकार नहीं है कि संसार में दुराचार, दुष्कर्म, अत्याचार, अन्याय और हत्या एवं विनाश का सिलसिला जारी रहे। वह पसन्द नहीं करता कि जो केवल उसके बन्दे हैं, उनको लोगों का बन्दा बनाकर उनके मानवीय गौरव पर अपमान का दाग़ लगाया जाए। अतः जो गिरोह बिना किसी बदले की इच्छा, बिना किसी धन-दौलत के लालच, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के केवल ईश्वर के लिए संसार को इस उपद्रव से मुक्त करने के लिए और इस अन्याय को दूर करके इसके स्थान पर न्याय स्थापित करने के लिए खड़ा हो जाए और इस सुकर्म में अपने जान और धन, अपने व्यापारिक लाभ, अपने बाल-बच्चों और बाप-भाइयों के प्रेम और अपने घर-बार के सुख और आराम सबको त्याग दे, उससे अधिक ईश्वर के प्रेम और ईश-प्रसन्नता का अधिकारी कौन हो सकता है और सफलता का द्वार उसके सिवा किसके लिए खुल सकता है?
ईश्वरीय मार्ग में जिहाद की यही विशिष्टता है जिसके कारण उसे समस्त मानवीय कर्मों में ईश्वर पर ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। और ध्यान से देखा जाए तो मालूम होगा कि वास्तव में यही चीज़ समस्त श्रेष्ठताओं और नैतिक विशिष्टताओं की आत्मा है। मनुष्य की यह भावना कि वह बुराई को किसी दशा में भी सहन न करे और उसे दूर करने के लिए हर प्रकार की कु़रबानी देने के लिए तैयार हो जाए, मानवीय गौरव की सबसे उच्च भावना है। और व्यावहारिक जीवन की सफलता का रहस्य भी इसी भावना ही में निहित है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुराई को सहन करता है, उसकी नैतिक दुर्बलता उसे अन्ततः इस पर भी आमादा कर देती है कि वह स्वयं अपने लिए बुराई को सहन करने लगे। और जब उसमें सहन कर यह गुण पैदा हो जाता है तो फिर वह इतना अधिक अपमानग्रस्त होता है जिसे ईश्वर ने अपने प्रकोप से अभिव्यंजित किया है:
‘‘और उन पर अपमान और हीन दशा थोप दी गई और वे ईश्वर के प्रकोप के भागी हुए।’’ (क़ुरआन, 2:61)
इस स्तर पर पहुँचकर मनुष्य के भीतर प्रतिष्ठा एवं मानवता का कोई एहसास बाक़ी नहीं रहता। वह शारीरिक एवं भौतिक दासता ही नहीं, बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक दासता में भी ग्रस्त हो जाता है और अधमता के ऐसे गढ़े में गिरता है जहाँ से उसका निकलना असम्भव हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में यह नैतिक शक्ति मौजूद हो कि वह बुराई को मात्रा बुराई होने के कारण बुरा समझे और मानव-जाति को उससे मुक्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहे, वह एक सच्चा और उच्च कोटि का मनुष्य होता है और उसका अस्तित्व मानव-जगत के लिए सर्वथा दयालुता होता है। ऐसे व्यक्ति को चाहे संसार से किसी बदले की इच्छा न हो, किन्तु दुनिया उन समस्त अकृतज्ञताओं के होते हुए जिनके दाग़ उसके माथे पर पाए जाते हैं, उपकार से इतनी अनभिज्ञ व उदासीन भी नहीं है कि वह मानवता के उस सेवक को अपना सरताज, अपना पेशवा और अपना नायक स्वीकार न कर ले जो बेलाग और प्रतिदान से निस्पृह होकर उसे बुराई के क़ब्ज़े से छुड़ाने और नैतिक एवं आध्यात्मिक और भौतिक स्वतंत्राता प्रदान करने के लिए अपना सब कुछ कु़रबान कर दे। इसी से इस आयत का अर्थ समझ में आता है, जिसमें कहा गया है कि ‘‘धरती के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे।’’ (क़ुरआन, 21:105); और यहीं से यह बात निकलती है कि ‘‘वही हैं जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं।’’ (क़ुरआन, 9:120); इससे अभिप्रेरत केवल परलोक ही की सफलता नहीं है, बल्कि संसार की सफलता भी वास्तव में उन्हीं लोगों के लिए है जो तुच्छ इच्छाओं से मुक्त होकर मात्र ईश-प्रसन्नता और ईश्वर के बन्दों की भलाई के लिए जिहाद करते हैं।
सामाजिक व्यवस्था में जिहाद का स्थान
जिहाद की इस वास्तविकता को जान लेने के पश्चात यह समझ लेना बहुत आसान है कि क़ौमों की ज़िन्दगी में इसको क्या स्थान प्राप्त है और सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है। यदि संसार में कोई ऐसी शक्ति मौजूद हो जो बुराई के विरुद्ध निरंतर जिहाद करती रहे और समस्त सरकश क़ौमों को अपनी-अपनी सीमा की पाबन्दी पर बाध्य कर दे तो सामाजिक व्यवस्था में यह असंतुलन कदापि दिखाई न दे कि आज सम्पूर्ण मानव-जगत अत्याचारियों और उत्पीड़ितों, आक़ाओं और ग़ुलामों में विभक्त है और सम्पूर्ण संसार में नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन कहीं दासता और अत्याचार के कारण और कहीं गु़लाम बनाने और दमनकारिता के कारण विनष्ट हो रहा है। बुराई को दूसरों से हटाना तो एक बड़ा दर्जा है, यदि उसे स्वयं अपने से हटाने का एहसास भी एक क़ौम में मौजूद हो और इसके मुक़ाबले में वह अपने सुख-विलास को, अपने धन-वैभव को, अपने ऐन्द्रिक आनन्दों और अपने जान के प्रेम को, सारांश यह कि किसी चीज़ को भी प्रिय न समझे तो वह कभी अपमानित होकर नहीं रह सकती और उसकी प्रतिष्ठा को कोई शक्ति रौंद नहीं सकती। सत्य के आगे सिर झुकाना और असत्य के आगे सिर झुकाने पर मृत्यु को प्राथमिकता देना एक प्रतिष्ठित क़ौम की विशेषता होनी चाहिए और यदि वह सत्य को उच्चता प्रदान करने और सत्य की सहायता की शक्ति न रखती हो तो उसे कम-से-कम सत्य की सुरक्षा पर दृढ़ता के साथ अवश्य अटल रहना चाहिए जो प्रतिष्ठा का कम-से-कम दर्जा है। किन्तु इस दर्जे से गिरकर जो क़ौम सत्य की रक्षा भी न कर सके और उसमें उत्सर्ग और कु़रबानी का अभाव इतना बढ़ जाए कि बुराई और दुष्टता जब उस पर चढ़कर आए तो वह उसे मिटाने या स्वयं मिट जाने के बजाय उसके अधीन जीवित रहने को स्वीकार कर ले तो ऐसी क़ौम के लिए दुनिया में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उसका जीवन निश्चय ही मृत्यु से निकृष्ट है। इसी रहस्य को समझाने के लिए ईश्वर ने बार-बार अपनी तत्वदर्शितापूर्ण पुस्तक में उन जातियों का उल्लेख किया है जिन्होंने बुराई के विरुद्ध जिहाद करने में जान, धन और ऐन्द्रिक सुखों का टोटा देखकर उससे जी चुराया और बुराई का अधिपत्य स्वीकार करके अपने ऊपर सदैव के लिए घाटा और असफलता का दाग़ लगा लिया। ऐसी क़ौमों को ईश्वर ज़ालिम क़ौमें कहता है। अर्थात् उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं अपने ऊपर जु़ल्म किया और वास्तव में वे अपने ही जु़ल्म से विनष्ट हुईं। अतएव एक स्थान पर इस प्रकार उनका उदाहरण दिया है:
‘‘क्या उन्हें उन लोगों का वृत्तांत नहीं पहुँचा जो उनसे पहले गुज़रे हैं—नूह के लोगों का, आद और समूद का, और इबराहीम की क़ौम का और मदयन वालों का और उन बस्तियों का जिन्हें उलट दिया गया? उनके रसूल उनके पास खुले-खुले मार्गदर्शन लेकर आए थे, फिर ईश्वर ऐसा न था कि वह उन पर अत्याचार करता, किन्तु वे स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे थे। रहे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वे सब परस्पर एक-दूसरे के सहयोगी हैं। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं।’’ (क़ुरआन, 9:70-71)
यहां पिछली क़ौमों के अपने आप पर जु़ल्म करने का उल्लेख करते ही जो ईमान वालों का यह गुण बताया है कि वे एक-दूसरे के मित्र और सहायक हैं और नेकी को क़ायम करते और बुराई को रोकते हैं तो इससे स्पष्टतः यही बताना अभीष्ट है कि उन मिटने वाली क़ौमों ने भलाई का हुक्म देना और बुराई को रोकना छोड़ दिया था। और यही उनका वह जु़ल्म था जिसने अंततः उनको तबाह किया।
एक और जगह ‘बनी-इसराईल’ की कायरता और जिहाद से जी चुराने के अत्यंत शिक्षाप्रद परिणाम का उल्लेख किया गया है। कहा कि मूसा (अलैहि॰) ने अपनी क़ौम को ईश्वर की अनुकम्पाओं का स्मरण कराकर आदेश दिया कि तुम पवित्रा भू-भाग में प्रवेश करो जिसे ईश्वर ने तुम्हारी मीरास में दिया है। और कदापि पीठ मत पे$री, क्योंकि पीठ पे$रने वाले सदैव असफल रहा करते हैं। किन्तु बनी-इसराईल पर भय छाया हुआ था। उन्होंने कहा:
‘‘ऐ मूसा! उस भूभाग में तो बड़े शक्तिशाली लोग रहते हैं। हम तो वहाँ कदापि नहीं जा सकते, जब तक कि वे वहाँ से निकल नहीं जाते। हाँ, यदि वे वहाँ से निकल जाएँ तो हम अवश्य प्रविष्ट हो जाएँगे।’’ (क़ुरआन, 5:22)
क़ौम के दो नवयुवकों ने, जिन पर ईश्वर ने कृपा की थी, क़ौम को परामर्श दिया कि तुम निर्भय होकर प्रवेश करो। तुम्हीं प्रभावी रहोगे। और यदि तुम्हें ईमान की दौलत प्राप्त है तो ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। किन्तु वे कायर और हीन दशा पर संतुष्ट रहने वाली क़ौम मनुष्यों के भय से काँपती ही रही और उसने साफ़ कह दिया कि:
‘‘ऐ मूसा! जब तक वे लोग वहाँ हैं, हम तो कदापि वहाँ नहीं जाएँगे। ऐसा ही है तो जाओ तुम और तुम्हारा रब, और दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे।’’
(क़ुरआन, 5:24)
अन्ततः इस कायरता के कारण ईशतेजस्विता ने यह निर्णय किया कि वे चालीस वर्ष तक इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहें और कहीं उनको ठिकाना न मिल सके। (ईश्वर ने) कहा:
‘‘अच्छा तो अब यह भूमि चालीस वर्ष तक इनके लिए वर्जित है। ये धरती में मारे-मारे फिरेंगे।’’ (क़ुरआन, 5:26)
एक दूसरी जगह विस्तारपूर्वक बनी-इसराईल के, अपनी जान और माल के साथ उस पे्रम और कायरता और मृत्यु के भय का उल्लेख किया गया है जिसके कारण उन्होंने ईश्वरीय मार्ग का जिहाद त्याग दिया और जिसके कारण अन्ततः वे क़ौमी विनाश में ग्रस्त हुए। कहा गया है:
‘‘क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में होने पर भी मृत्यु के भय से अपने घर-बार छोड़कर निकले थे? तो ईश्वर ने उन पर मौत ही का आदेश भेज दिया। फिर उसने उन्हें दोबारा जीवन प्रदान किया। वास्तविकता यह है कि ईश्वर तो लोगों के लिए उदार अनुग्राही है, किन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते।’’ (क़ुरआन, 2:243)
इसके बाद ही इस तरह मुसलमानों को लड़ने का आदेश दिया है:
‘‘ईश्वर के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि ईश्वर ख़ूब सुनने और जानने वाला है।’’ (क़ुरआन, 2:244)
और इसके बाद पुनः इसराईल के गिरोह का उल्लेख किया है:
‘‘क्या तुमने मूसा के पश्चात् इसराईल की संतान के सरदारों को नहीं देखा, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा: ‘हमारे लिए एक सम्राट नियुक्त कर दो, ताकि हम ईश्वर के मार्ग में युद्ध करें?’ नबी ने कहा: ‘यदि तुम्हें कोई लड़ाई का आदेश दिया जाए तो क्या तुम्हारे बारे में यह संभावना नहीं है कि तुम न लड़ो?’ वे कहने लगे: ‘हम ईश्वर के मार्ग में क्यों न लड़ेंगे जबकि हम अपने घरों से निकाल दिए गए हैं और अपने बाल-बच्चों से भी अलग कर दिए गए हैं?’—फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से थोड़े लोगों के सिवा सबके सब फिर गए। और ईश्वर ज़ालिमों को भली-भांति जानता है।’’ (क़ुरआन, 2:246)
यह और ऐसे बहुत-से उदाहरण बार-बार इसी तथ्य को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि भलाई की स्थापना और उसके स्थायित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उसकी रक्षा करने वाले सच्चे उत्सर्ग की आत्मा है और जिस क़ौम से यह आत्मा विदा हो जाती है वह बहुत जल्द बुराई से पराजित होकर विनष्ट हो जाती है।
----------------------------
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
HindiIslamMail@gmail.com
Subscribe Our You Tube Channel
https://www.youtube.com/c/hindiislamtv
----------------------------
ऊपर पोस्ट की गई किताब ख़रीदने के लिए संपर्क करें:
MMI Publishers
D-37 Dawat Nagar
Abul Fazal Enclave
Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 011-26981652, 011-26984347
Mobile: +91-7290092401
https://www.mmipublishers.net/
Recent posts
-

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024 -
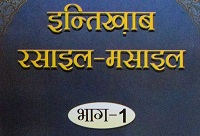
इंतिख़ाब रसाइल-मसाइल (भाग-1)
19 March 2024 -

प्यारी माँ के नाम इस्लामी सन्देश
18 March 2024 -

इस्लाम की गोद में
17 March 2024 -

शान्ति-मार्ग
17 March 2024

