
इस्लाम की जीवन व्यवस्था
-
इस्लाम
- at 22 March 2020
मानव के अन्दर नैतिकता की भावना एक स्वाभाविक भावना है जो कुछ गुणों को पसन्द और कुछ दूसरे गुणों को नापसन्द करती है। यह भावना व्यक्तिगत रूप से लोगों में भले ही थोड़ी या अधिक हो किन्तु सामूहिक रूप से सदैव मानव-चेतना ने नैतिकता के कुछ मूल्यों को समान रूप से अच्छाई और कुछ को बुराई की संज्ञा दी है। सत्य, न्याय, वचन-पालन और अमानत को सदा ही मानवीय नैतिक सीमाओं में प्रशंसनीय माना गया है और कभी कोई ऐसा युग नहीं बीता जब झूठ, जु़ल्म, वचन-भंग और ख़ियानत को पसन्द किया गया हो। हमदर्दी, दयाभाव, दानशीलता और उदारता को सदैव सराहा गया तथा स्वार्थपरता, क्रूरता, कंजूसी और संकीर्णता को कभी आदर योग्य स्थान नहीं मिला। इससे मालूम हुआ कि मानवीय नैतिकताएं वास्तव में ऐसी सर्वमान्य वास्तविकताएँ हैं जिन्हें सभी लोग जानते हैं और सदैव जानते चले आ रहे हैं। अच्छाई और बुराई कोई ढकी-छिपी चीज़ें नहीं हैं कि उन्हें कहीं से ढूँढ़कर निकालने की आवश्यकता हो। वे तो मानवता की चिरपरिचित चीज़ें हैं जिनकी चेतना मानव की प्रकृति में समाहित कर दी गई है। यही कारण है कि क़ुरआन अपनी भाषा में नेकी और भलाई को ‘मारूफ़’ (जानी-पहचानी हुई चीज़) और बुराई को ‘मुनकर’ (मानव की प्रकृति जिसका इन्कार करे) के शब्दों से अभिहित करता है। हमदर्दी, दया भाव, दानशीलता और उदारता को सदैव सराहागया तथा स्वार्थपरता, क्रूरता, कंजूसी और संकीर्णता को कभी आदरयोग्य स्थान नहीं मिला। धैर्य, सहनशीलता, स्थैर्य, गंभीरता, दृढसंकल्पित व बहादुरी वे गुण हैंजो सदा से प्रशंसनीय रहे है। -संपादक
मौलाना सैयद अबुलआला मौदूदी
मानव समाज में धैर्य, सहनशीलता, स्थैर्य, गंभीरता, दृढ़संकल्पता व बहादुरी वे गुण हैं जो सदा से प्रशंसनीय रहे हैं। इसके विपरीत धैर्यहीनता, क्षुद्रता, विचार की अस्थिरता, निरुत्साह और कायरता पर कभी भी श्रद्धा-सुमन नहीं बरसाए गए। आत्मसंयम, स्वाभिमान, शिष्टता और मिलनसारी की गणना सदैव उत्तम गुणों में ही होती रही और कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोग-विलास, ओछापन और अशिष्टता ने नैतिक गुणों की सूची में कोई जगह पाई हो। कर्तव्यपरायणता, विश्वसनीयता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व की भावना का सदा सम्मान किया गया तथा कर्तव्य विमुख, धोखाबाज़, कामचोर तथा ग़ैर ज़िम्मेदार लोगों को कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। इसी प्रकार सामूहिक जीवन के सदगुणों व दुर्गुणों के मामले में भी मानवता का फ़ैसला एक जैसा रहा है। प्रशंसा की दृष्टि से वही समाज देखा गया है जिसमें अनुशासन और व्यवस्था हो, आपसी सहयोग तथा सहकारिता हो, आपसी प्रेमभाव तथा हितचिन्तन हो, सामूहिक न्याय व सामाजिक समानता हो। आपसी फूट, बिखराव, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, मतभेद, परस्पर द्वेषभाव, अत्याचार और असमानता की गणना सामूहिक जीवन के प्रशंसनीय लक्ष्णों में कभी भी नहीं की गई। ऐसा ही मामला चरित्रा की अच्छाई और बुराई का भी है। चोरी, व्यभिचार, हत्या, डकैती, धोखाधड़ी और घूसख़ोरी कभी सत्कर्म नहीं माने गए। अभद्र भाषण, उत्पीड़न, पीठ पीछे बुराई, चुग़लख़ोरी, ईर्ष्या, दोषारोपण तथा उपद्रव फैलाने को कभी ‘पुण्य’ नहीं समझा गया। मक्कार, घमंडी, आडम्बरवादी, कपटाचारी, हठधर्म और लोभी व्यक्ति कभी भले लोगों में नहीं गिने गए। इसके विपरीत माँ-बाप की सेवा, संबंधियों की सहायता, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार, मित्रों से हमदर्दी, निर्बलों की हिमायत, अनाथों और बेसहारों की देखरेख, रोगियों की सेवा तथा पीड़ितों की मदद सदैव नेकी समझी गई है। स्वच्छ चरित्र वाला मधुर-भाषी, विनम्र-भाव व्यक्ति और सब की भलाई चाहने वाले लोग सदा आदरणीय रहे। मानवता उन्हीं लोगों को अपना उत्तम अंश मानती रही है जो सच्चे और शुभ-चिन्तक हों, जिन पर हर मामले में भरोसा किया जा सके, जिनका बाहर और भीतर एक समान हो, जिनकी कथनी करनी में समानता हो, जो अपने हितों की प्राप्ति में संतोष करने वाले और दूसरों के अधिकारों और हितों को देने में उदार हृदय हों, शान्तिपूर्वक रहें और दूसरों को शान्ति प्रदान करें, जिनके व्यक्तित्व से प्रत्येक को ‘भलाई’ की आशा हो और किसी को बुराई की आशंका न हो।
इससे मालूम हुआ कि मानवीय नैतिकताएं वास्तव में ऐसी सर्वमान्य वास्तविकताएं हैं जिन्हे सभी लोग जानते हैं और सदैव जानते चले आ रहे हैं। अच्छाई और बुराई कोई ढकी-छिपी चीज़ नही हैं कि उन्हे कहीं से ढूॅढकर निकालने की आवश्यकता हो। वे तो मानवता की चिरपरिचित चीज़ें हैं जिनकी चेतना मानव की प्रकृति में समाहित कर दी गई हैं। यही कारण हैं कि कुरआन अपनी भाषा में नेकी और भलाई को ‘मारूफ' (जानी-पहचानी हुई चीज़) और बुराई को ‘मुनकर' (मानव की प्रकृति जिसका इनकार करे) के शब्दों से अभिहित करता हैं।
अर्थात भलाई और नेकी वह चीज़ हैं जिसे सभी लोग भला जानते हैं और ‘मुनकर' वह हैं जिसे कोई अच्छाई और भलाई के रूप में नही जानता। इसी वास्तविकता का कुरआन दूसरे शब्दों में इस प्रकार वर्णन करता है:
इस्लाम का जवाब यह है कि इस सृष्टि का स्वामी ईश्वर है और वह एक ही स्वामी है। उसी ने इस सृष्टि को पैदा किया। वही इसका एकमात्र प्रभु, शासक और पालनहार है। उसी के आदेशानुपालन के कारण यह सारी व्यवस्था चल रही है। वह तत्वदर्शी, सर्वशक्तिमान हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष का जानने वाला हैं। सभी दोषो, भूलों, निर्बलताओं तथा कमियों से मुक्त हैं। उनकी व्यवस्था मे लागलपेट या टेढ़ापन बिलकुल नही हैं। मनुष्य उसका जन्मजात बन्दा (दास) है। उसका कार्य यही है कि वह अपने स्रष्टा की बन्दगी (ग़ुलामी) और आज्ञापालन करे।
उसके जीवन का लक्ष्य ईश्वर के प्रति समर्पण और आज्ञापालन है जिनकी पद्धति निर्धारित करना मनुष्य का अपना काम नही बल्कि उस ईश्वर का काम है जिसका वह दास हैं। ईश्वर ने उसके मार्गदर्शन हेतु अपने दूत (पैगम्बर) भेजे हैं और ग्रन्थ उतारे है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी जीवन-व्यवस्था इसी ईश्वरीय मार्गदर्शन के स्रोत से प्राप्त करे। मनुष्य अपने सभी कार्यकलापों के लिए ईश्वर के सामने उत्तरदायी हैं और इस उत्तरदयित्व के सम्बन्ध में उसे इस लोक में नही बल्कि परलोक मे हिसाब देना है। वर्तमान जीवन तो वास्तव मे परीक्षा की अवधि है। इसलिए यहां मनुष्य के सम्पूर्ण प्रयास इस लक्ष्य की ओर केन्द्रित होने चाहिए कि वह आखिरत की जवाबदेही में अपने प्रभु के समक्ष सफल हो जाए। परलोक की इस परीक्षा मे मनुष्य अपने पूरे अस्तित्व के साथ सम्मिलित है। उसकी सभी शक्तियों एवं योग्यताओं की परीक्षा है। पूरे विश्व की जो चीजे भी मनुष्य के सम्पर्क में आती है उसके बारे में निष्पक्ष जांच होती है कि मनुष्य ने उन चीज़ों के साथ कैसा मामला किया और यह जॉच करनेवाली वह सत्ता है जिसने धरती के कण-कण पर, हवा और पानी, विश्वात्मक तरंगो पर और ख़ुद इन्सान के दिल व दिमाग और हाथ-पैर पर, उसकी गतिविधियों का ही नहीं बल्कि उसके विचारों तथा इरादों तक का ठीक-ठीक उपलब्ध कर रखा है।
यह है वह उत्तर जो इस्लाम ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों का दिया है। सृष्टि और मनुष्य के संबंध मे उक्त अवधारणा उस वास्तविक और परम कल्याण के लक्ष्य को निर्धारित कर देती हैं जिसे प्राप्त करने का भरपूर प्रयास मनुष्य को करना चाहिए, और वह है ईश्वर की प्रसन्नता। यही वह मानदण्ड है जिसपर इस्लाम की नैतिक व्यवस्था में किसी कार्य शैली को परखकर यह निर्णय किया जाता है कि वह ‘भला' है या ‘बुरा'। इसके निर्धारिण से नैतिकता को वह धुरी मिल जाती है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण नैतिक जीवन धूमता है और उसकी स्थिति लंगर रहित जहाज़ की-सी नही रहती कि हवा के झोंके और समुन्द्र की लहरों के थपेड़े उसे इधर-उधर दौड़ते फिरें । यह निर्धारण एक केन्द्रिय उद्देश्य सामने रखता हैं जिसके परिणामस्वरूप जीवन मे सभी नैतिक गुणों की उचित सीमाएं उचित स्थान और उपयुक्त व्यावहारिक रूप निश्चित हो जाते हैं। हमे वह स्थायी मूल्य मिल जाते हैं जो परिवर्तनशील परिस्थितियों मे भी अपनी जगह अटल रह सकें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ईश प्रसन्नता का लक्ष्य प्राप्त कर लेने से नैतिकता को एक उच्चतम परिणाम मिल जाता है जिसके फलस्वरूप नैतिक उत्थान की सम्भावनाएं असीम हो जाती हैं और किसी चरण में भी स्वार्थपरता का प्रदूषण उसे दूषित नहीं कर सकता।
मापदण्ड प्रदान करने के साथ इस्लाम अपने इसी विश्व तथा मानव अवधारणा पर आधारित नैतिक सौन्दर्य तथा असौन्दर्य के ज्ञान का एक स्थायी स्रोत भी हमे प्रदान करता है। उसने हमारे नैतिकता के ज्ञान को मात्र हमारी बृद्धि या इच्छाओं या अनुभवों अथवा मानवीय ज्ञान के भरोसे नही छोड़ा हैं कि यदि से चीजें अपने निर्णय बदल दे तो हमारे नैतिक सिद्धान्त भी बदल जाएं और उन्हे कोई स्थायित्व न मिल सके, बल्कि इस्लाम ने हमें दो निश्चित स्रोत (ईशग्रन्थ और ईशदूत का आदर्श) प्रदान किए हैं जिससे हमे हर युग तथा प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक निर्देश प्राप्त होते हैं। ये निर्देश ऐसे व्यापक हैं कि घरेलू जीवन के छोटे से छोटे मामलात से लेकर बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समस्याओं तक जीवन के हर पक्ष और प्रत्येक विभाग में वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके अन्दर जीवन संबंधी विषयों पर नैतिक सिद्धान्तों का वह व्यापक निरूपण (Widest Application) पाया जाता हैं जो किसी स्तर पर किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही प्रतीत नही होने देता।
सृष्टि व मानव सम्बन्धी इस्लाम की इसी अवधारणा में वह क्रियान्वयन शक्ति (Sanction) भी मौजूद है जिसका होना नैतिक क़ानून को लागू करने के लिए जरूरी है और वह है ईशभय, परलोक की पूछताछ का डर और शाश्वत भविष्य की असफलता का खतरा । यद्यपि इस्लाम एक ऐसी शक्ति और जनमत (Public Opinion) भी तैयार करना चाहता है जो सामाजिक जीवन में व्यक्तियों एवं समुदायों को नैतिक नियमों की पाबन्दी पर विवश करने वाले हों और एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था भी बनाना चाहता है जिसके द्वारा नैतिकता संबंधी आचार संहिता बलपूर्वक लागू करे परन्तु इसमे दबाव की अपेक्षा आन्तरिक प्रेरणा अधिक शक्तिशाली हो जो ईश्वर और परलोक के विचार पर आधारित हो। नैतिकता संबंधी निर्देश देने से पहले इस्लाम आदमी के दिल में यह बात बिठाता है कि तेरा मामला वास्तव में उस अल्लाह के साथ है जो हर समय हर जगह तुझे देख रहा है। तू दुनिया भर से छिप सकता है मगर उससे नही छिप सकता। दुनिया भर को धोखा दे सकता है मगर उसे धोखा नहीं दे सकता। दुनिया भर से भाग सकता है मगर उसकी पकड़ से बचकर कही नही जा सकता। दुनिया केवल तेरा बाहरी रूप देख सकती है मगर ईश्वर मेरी नीयत तथा तेरे इरादों तक को देख लेता है। दुनिया के थोड़े से जीवन मे तू जो चाहे कर ले मगर तुझे अन्तत: मरकर उसकी अदालत मे उपस्थित होना है जहां वकालत, रिश्वत, सिफारिश, झूठी गवाही, धोखा कुछ भी न चल सकेगा और तेरे भविष्य का निष्पक्ष फैसला हो जाएगा। इस विश्वास के द्वारा इस्लाम मानो हर व्यक्ति के दिल में पुलिस की एक चौकी स्थापित कर देता है जो अन्दर से उसको आदेश पालन पर विवश करती हैं। चाहे बाहर उन आदेशों की पाबन्दी करानेवाली पुलिस,अदालत और जेल मौजूद हो या न हो। इस्लाम के नैतिक कानून के पीछे यहां वास्तविक शक्ति है जो उसे लागू कराती है। जनमत और शासन का समर्थन भी इसे प्राप्त हो तो कहना ही क्या ! वरना मात्र यही ईमान और विश्वास मुसलमानों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सीधा चला सकता है शर्त यही हैं कि सच्चा ईमान दिलों मे बैठा हुआ हो।
इस्लाम की राजनीतिक व्यवस्था
इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद तीन सिद्धान्तों पर रखी गई हैं। तौहीद, रिसालत और खिलाफत । इन सिद्धान्तो को भली-भांति समझे बिना इस्लामी राजनीति की विस्तुत व्यवस्था को समझना कठिन है। इसलिए सर्वप्रथम इन्हीं की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत है।
तौहीद (एकेश्वरवाद) का अर्थ यह हैं कि ईश्वर इस संसार और इसमें बसने वालों का स्रष्टा, पालक और स्वामी है। सत्ता और शासन उसी का है। वही हुक्म देने और मना करने का हक़ रखता है। आज्ञापालन तथा पूर्णसमर्पण केवल उसी के लिए है। हमारा यह अस्तित्व, हमारे ये शारीरिक अंग एवं शक्तियां जिनसे हम काम लेते है, हमारे उपयोग की वस्तुएं तथा उनसे संबंधित हमारे अधिकार जो हमें संसार की सभी चीजों पर प्राप्त हैं और स्वंय वे चीजें जिन पर हमारा अधिकार है, उनमें से कोई चीज़ भी न हमारी पैदा की हुई है और न हमने उसे प्राप्त किया है, सबकी ईश्वर द्वारा ही पैदा की गई हैं और उसी ने हमें सब कुछ प्रदान किए हैं, जिसमें अन्य कोई हस्ती भागीदार नही है। इसलिए अपने अस्तित्व का उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का प्रयोजन और अपने अधिकारों का सीमा-निर्धारण करना न तो हमारा अपना कार्य है और न किसी अन्य व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है, यह केवल उस ईश्वर का कार्य है जिसने हमको इन शक्तियों तथा अधिकारों के साथ पैदा किया और दुनिया की बहुत-सी चीज़ें हमारे अधिकार में दी हैं। यह सिद्धान्त मानवीय प्रभुसत्ता (Sovereignty) को पूर्ण रूपेण नकार देता है। एक इन्सान हो या एक परिवार, एक वर्ग हो या एक समुदाय अथवा पूरी दुनिया के लोग हों किसी को प्रभुसत्ता का अधिकार नहीं। हाकिम (सम्प्रभु) केवल अल्लाह है, उसी का हुक्म ‘क़ानून' है।
इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था
इनसान के आर्थिक जीवन को इन्साफ़ और सच्चाई पर बनाए रखने के लिए इस्लाम ने कुछ सिद्धान्त और सीमाएं निर्धारित कर दी हैं, ताकि धन की उत्पत्ति, उपयोग और वितरण (Circulation) की सम्पूर्ण व्यवस्था उन्हीं सीमा रेखाओं के अन्तर्गत चले जो उसके लिए खींच दी गई हैं।
धनोपार्जन की विधियां और उसके वितरण के रूप क्या हों, इस्लाम की इस प्रश्न से कोई रूचि नहीं है। ये चीजें तो विभिन्न युगों में सभ्यता के विकास के साथ-साथ बनती और बदलती रहती है। उनका निर्धारण मानव की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ख़ुद ही हो जाता हैं। इस्लाम जो कुछ चाहता है वह यह है कि सभी युगों और परिस्थितियों में मानव की आर्थिक क्रियाएं जो रूप भी धारण करें उनमें ये सिद्धान्त स्थायी रूप से लागू रहे और उन निर्घारित प्रतिबन्दों का अनिवार्यत: पालन किया जाए।
इस्लामी दृष्टिकोण से धरती तथा उस पर स्थित सभी चीजे ईश्वर ने मानव-जाति के लिए बनाई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि धरती से अपनी आजीविका प्राप्त करने का यत्न करें। इस अधिकार में सभी मानव समान रूप से भागीदार है, किसी को इस अधिकार से वंचित नही किया जा सकता और न किसी को इस सम्बन्ध में दूसरों की तुलना में प्राथमिकता ही प्राप्त हो सकती है। किसी व्यक्ति या जाति या वर्ग पर ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नही लगाया जा सकता जिससे वह आर्थिक संसाधनों में से कुछ को इस्तेमाल करने का अधिकारी ही न रहे, अथवा कुछ पेशों का द्वार उसके लिए बन्द कर दिया जाए। इसी प्रकार ऐसे भेदभाव भी धार्मिक नियम के आधार पर नही बरते जा सकते जिनके आधार पर किसी आर्थिक संसाधन या आजीविका के साधन पर किसी विशेष वर्ग या जाति या परिवार का एकाधिकार स्थापित हो जाए। ईश्वर की बनाई हुई धरती पर उसके पैदा किए हुए संसाधनों में से अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश करना सब इन्सानों का समान अधिकार है। सभी को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए।
प्रकृति की जिन नेमतों को उपयोगी बनाने में किसी के परिश्रम तथा योग्यता का प्रयोग न हो उन पर सभी लोगो को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उनसे अपनी आवश्यकतानुसार लाभान्वित हो। नदियों और झरनो का पानी, जंगल की लकड़ी , प्राकृतिक रूप से उगनेवाले पेड़ो के फल, स्वतन्त्ररूप से उगी घास और चारा हवा, पानी, मरूभूमि के जानवर, धरती की सतह पर खुली हुई खाने आदि पर न तो किसी का एकाधिकार स्थापित हो सकता हैं और न ही ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं कि आम जनता कुछ भुगतान किए बिना उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी न कर सके। हां जो लोग व्यावसायिक उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उनमें से किसी चीज को उपयोग में लाना चाहे तो उनपर टैक्स लगाया जा सकता है।
ईश्वर ने जो चीज़ें इन्सान के लाभ के लिए बनाई हैं उन्हे बेकार डाल देना उचित नही है। या तो उनसे स्वंय लाभ उठाओ या फिर दूसरों को लाभ उठाने के लिए छोड़ दो। इसी सिद्धान्त के आधार पर क़ानून यह निर्णय करता है कि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को तीन वर्ष से अधिक अवधि तक बेकार नही रख सकता। यदि वह उसको कृषि या भवन निर्माण अथवा किसी दूसरे प्रयोजन में न लाए तो तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात वह परित्यक्त भूमि समझी जाएगी। अन्य कोई व्यक्ति उसे अपने काम मे ले आए तो उसपर आपत्ति नही की जाएगी और इस्लामी प्रशासन को भी यह अधिकार होगा कि ऐसी भूमि किसी को आवंटित कर दे।
जो व्यक्ति सीधे प्रकृति के ख़ज़ाने में से किसी चीज को लेकर अपने परिश्रम तथा अपनी योग्यता से उसको उपयोगी बनाए तो वह उस वस्तु का मालिक है। उदाहरणार्थ किसी बेकार पड़ी ज़मीन को जिसपर किसी का स्वामित्व साबित न हो, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार मे लेकर किसी लाभकारी कार्य में इस्तेमाल करने लगे तो उसे बेदख़ल नही किया जा सकता। इस्लामी दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया में स्वामित्व सम्बन्धी सभी अधिकारों की शुरूआत इसी प्रकार हुई है। पहले पहल जब पृथ्वी पर इन्सानी आबादी आरम्भ हुई तो सभी चीज़ें सब लोगो के प्रयोग के लिए आम थी। फिर जिस व्यक्ति ने किसी आम चीज़ को अपने अधिकार मे लेकर किसी प्रकार उपयोगी बना लिया तो वह उसका मालिक हो गया। अर्थात उसे यह अधिकार प्राप्त हो गयाा कि वह उसे अपने लिए आरक्षित कर ले और दूसरे लोग यदि उसको प्रयोग करना चाहे तो उनसे बदले में धन प्राप्त करे। यह चीज़ मनुष्य के सारे आर्थिक मामलों की स्वाभाविक बुनियाद है और इस बुनियाद को यथा स्थिति बना रहना चाहिए।
इस्लाम केवल इतना ही नहीं चाहता कि सामाजिक जीवन मे यह आर्थिक दौड़ खुली और निष्पक्ष हो बल्कि यह भी चाहता है कि इस मैदान में दौड़ने वाले एक दूसरे के लिए निर्दयी और निष्ठुर न हों, हमदर्द और मददगार हों । इस्लाम एक ओर तो अपनी नैतिक शिक्षा से लोगो में यह भावना उजागर करता है कि वे अपने दबे और पिछड़े भाइयों को सहारा दें तथा दूसरी ओर वह मांग करता है कि सोसाइटी में एक स्थायी संस्था ऐसी मौजूद रहे जो अपंग लोगो की सहायता का जिम्मा ले। जो लोग आर्थिक दौड़ में भाग लेने योग्य न हों वे इस संस्था से अपना हिस्सा पाएं। जो लोग परिस्थिति और संयोगवंश इस दौड़ में गिर पड़े हो उन्हे यह संस्था उठाकर फिर चलने योग्य बनाए और जिन लोगो को संघर्ष में उतरने के लिए सहारे की आवश्यकता हो उन्हे इस संस्था से सहारा मिले। इस उद्देश्य के लिए इस्लाम ने क़ानून के आधार पर यह निश्चित किया है कि देश के धन की कुल जमा राशि तथा सम्पूर्ण व्यापारिक पूंजी पर ढाई प्रतिशत वार्षिक ज़कात (Poor Due) वसूल की जाएं। सभी कृषि-भूमि की उपज का पांच या दस प्रतिशत, कुछ खनिज पदार्थों की उपज का बीस प्रतिशत भाग वसूल किया जाए। पशुओं की एक निश्चित संख्या में से एक निश्चित अनुपात में वार्षिक ज़कात निकाली जाए और यह सम्पूर्ण धन निर्धनों, अनाथों तथा असम्पन्न लोगो की सहायतार्थ इस्तेमाल किया जाए। यह एक ऐसा ‘सामूहिक बीमा' हैं जिसकी उपस्थिति मे ईस्लामी सोसाइटी में कोई व्यक्ति जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं से कभी वंचित नही रह सकता। कोई श्रमिक कभी इतना मजबूर नही हो सकता कि भूखों मरने के डर से मजदूरी की वही शर्ते मान ले जो फैक्ट्री मालिक या जमींदार पेश कर रहा है। ज़कात की इस व्यवस्था की मौजूदगी में किसी व्यक्ति की शक्ति उस न्यूनतम स्तर से कभी नीचे नही गिर सकती जो आर्थिक दौड़ में भाग लेने के लिए आवश्यक हैं।
इस्लाम की आध्यात्मिक व्यवस्था
इस्लाम की आध्यात्मिक व्यवस्था क्या है और सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्था से उसका क्या संबंध है? इस प्रश्न को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम आध्यात्म की इस्लामी अवधारणा तथा अन्य धर्मो और दार्शनिक प्रणालियों की अवधारणाओं के अन्तर को समझ ले। यह अन्तर स्पष्ट न होने के कारण अधिकतर ऐसा होता हैं कि इस्लाम की आध्यात्मिक व्यवस्था पर चर्चा करते हुए आदमी के दिमाग़ में बिना इरादे के वह अवधारणाएं धूमने लगती हैं जो प्राय: ‘रूहानियत' या ‘अध्यात्म' शब्द के साथ जुड़ गई हैं। फिर इस उलझन में पड़कर आदमी के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि इस्लाम की यह आध्यात्मिक व्यवस्था किस प्रकार की है जो आत्मा के जाने-पहचाने क्षेत्र से निकलकर भौतिकता तथा शारीरिक क्षेत्र में दख़ल देती है और केवल दख़ल ही नही देती बल्कि उसपर शासन करना चाहती है।
दर्शन ओर धर्म की दुनिया में साधारणतया जो विचार पाया जाता है वह यह है कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के प्रतिरोधी हैं, दोनो की दुनिया अलग-अलग हैं, दोनो की मांगे अलग बल्कि परस्पर विरोधी हैं। इन दोनो का विकास एक साथ संभव नही है। आत्मा के लिए शरीर और पदार्थ की दुनिया एक बन्दीगृह है।
सांसारिक जीवन के संबंध और आकर्षण वे हथकड़िया और बेड़ियां हैं जिनमें आत्मा जकड़ जाती है। दुनिया के कारोबार और क्रियाएं वह दलदल हैं जिसमें फंसकर आत्मा की उड़ान समाप्त हो जाती हैं। इस सोच का अनिवार्यत: परिणाम यह हुआ कि आध्यात्मिकता तथा सांसारिकता के मार्ग एक दूसरे से बिलकुल अलग हो गए। जिन लोगों ने दुनियादारी अपनाई वह पहले पग पर ही निराश हो गए कि यहां रूहानियत उनके साथ न चल सकेगी। इस चीज़ ने उन्हे भौतिकता मे डुबो दिया। जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तात्पर्य यह कि सांसारिक जीवन के सारे अंग अध्यात्म के प्रकाश से वंचित रह गए। परिणामस्वरूप पृथ्वी अत्याचार से भर गई । दूसरी ओर जो लोग अध्यात्म प्रेमी हुए उन्होने अपने आत्मिक उत्थान के लिए ऐसे मार्ग चुने जो दुनिया के बाहर ही बाहर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से आत्मिक उन्नति का कोई ऐसा मार्ग संभव ही न था जो दुनिया के अन्दर से होकर गुज़रता हो। उनके निकट आत्मा की उन्नति के लिए शरीर को कमज़ोर करना जरूरी था इसलिए उन्होने ऐसी तपस्याएं ईजाद कीं जो नफ़्स (वासना) को मारने और शरीर को चेतनाशून्य और बेकार कर देनेवाली हो। तपस्या के लिए उन्होने जंगलो, पहाड़ों और एकान्तवास को अत्यन्त उपयुक्त स्थान समझा ताकि आबादी का कोलाहल ज्ञान-ध्यान में विध्न न डालने पाए। आत्मिक विकास के लिए उन्हे इसके अतिरिक्त कोई उपाय न सूझा कि संसार तथा उसकी गतिविधियों से हाथ खींच लें तथा उन सभी संबंधों को काट फेकें जो उन्हें भौतिक संसार से जोड़े हुए हैं।
शरीर और आत्मा के इस परस्पर विरोध ने इन्सान के लिए उन्नति के शिखर के दो भिन्न-भिन्न अर्थ एवं लक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। सांसारिक जीवन की उन्नति का सर्वोच्च बिन्दु यह निश्चित हुआ कि इन्सान केवल भौतिक सुख-सुविधाओं से मालामाल हो, और अन्तिम लक्ष्य यह ठहरा कि मनुष्य एक अच्छा पंछी, एक बढ़िया मगरमच्छ, एक श्रेष्ठ घोड़ा और एक सफ़ल भेड़िया बन जाए। दूसरी ओर आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई यह तय हुई कि इन्सान कुछ अलौकिक शक्तियां का मालिक बन जाए और लक्ष्य यह ठहरा कि एक अच्छा रेडियो सेट, एक शक्तिशाली दूरबीन और एक बढ़िया माइक्रोस्कोप बन जाए अथवा नजर और उसके शब्द एक पूर्ण औषधालय का काम देने लगे।
इस्लाम का दृष्टिकोण इस मामले मे दुनिया की सभी धार्मिक व दार्शनिक व्यवस्थाओं से भिन्न है। वह कहता है कि इन्सानी आत्मा को ईश्वर ने धरती पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसे सौंपे है और उनको पूरा करने के लिए श्रेष्ठतम एवं उपयुक्ततम शारीरिक संरचना प्रदान की है। यह शरीर उसको दिया ही इसलिए गया है कि वह अपने अधिकारों के प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों के निर्वाह में उससे काम ले। इसलिए यह शरीर आत्मा के लिए जेल नही बल्कि उसका कारखाना है और यदि आत्मा का कोई विकास संभव है तो वह इसी प्रकार कि इस कारखाने के औजारों तथा उर्जा का उपयोग करके अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करे। फिर यह दुनिया कोई यातनागृह भी नही है जिसमें इन्सानी आत्मा किसी प्रकार आकर फैंस गई हो, बल्कि यह तो वह कर्मस्थली है जिसमें काम करने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा हैं। यहां कि अनगिनत चीज़ें उसके अधीन कर दी गई हैं। यहां दूसरे बहुत-से इन्सान इसी ख़िलाफ़त (प्रतिनिधित्व) के कर्तव्य निभाने के लिए उसके साथ पैदा किए गए हैं। यहां प्रकृति की मांगों से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा जीवन के अन्य विभाग उसके लिए अस्तित्व में आए हैं। यहां अगर कोई रूहानी तरक्की संभव है तो उसका उपाय यह नही हैं कि आदमी इस कर्मस्थली से मुख मोड़कर किसी एकान्त में जा बैठे, बल्कि उसका उपाय यह है कि वह इसके अन्दर कार्य करके अपनी योग्यता का परिचय दे। यह उसके लिए परीक्षा-भवन है। जीवन का प्रत्येक पक्ष परीक्षा के प्रश्न-पत्र के समान है। घर, मुहल्ला, बाजार, मंडी, दफ़तर, कारख़ाना, पाठशाला, कचहरी, थाना, छावनी, पार्लियामेन्ट, अमन कान्फ्रेन्स, (शांति सम्मेलन) और युद्ध के मैदान सब विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र हैं जो उसे करने के लिए दिए गए हैं। वह अगर उनमें से कोई प्रश्न पत्र न करे या अधिकतर विषयों की उत्तरपुस्तिका खाली छोड़ दे तो परीक्षाफल में शून्य के अतिरिक्त और क्या पा सकता है?
सफलता और उन्नति की संभावना अगर हो सकती है तो इसी तरह कि वह अपना सारा समय और पूरा ध्यान परीक्षा देने पर केन्द्रित करे और जितने पर्चे भी उसे दिए जाएँ उन सबमें कुछ करके दिखाए।
इस प्रकार इस्लाम ‘सन्यास' के विचार को रद् कर देता है और मानव के लिए आत्मिक उत्थान का मार्ग दुनिया के बाहर से नही बल्कि दुनिया के अन्दर से निकालता है। आत्मा की उन्नति, विकास और सफलता प्राप्ति का वास्तविक स्थान उसके अनुसार जीवन की गतिविधियों के ठीक बीच मे है, न कि उसके किनारे पर।
अब मै संक्षेप मे आपको बताउंगा कि इस्लाम सांसारिक जीवन के बीच से इन्सान के आत्मिक उत्थान का मार्ग किस प्रकार बनाता हैं।
1-इस मार्ग की प्रथम चरण ईमान है, जिसका आशय यह है कि आदमी के मन-मस्तिष्क मे यह बात बैठ जाए कि ईश्वर ही उसका मालिक, शासक, और पूज्य है। ईश-प्रसन्नता ही उसके सारे प्रयत्नों का मूल उद्देश्य हो और ईश्वर का आदेश ही उसके जीवन का विधान हो। यह विचार जितना अधिक दृढ़ और पक्का होगा उतनी ही अधिक इस्लामी मानसिकता पूर्णता लिए होगी और उतने ही स्थायित्व और दृढ़ निश्चय के साथ इन्सान आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकेगा।
2-इस रास्ते की दूसरी मंजिल आज्ञापालन है। अर्थात मनुष्य का व्यवहारत: अपनी स्वतन्त्रता को त्याग देना और उस ईश्वर के प्रति व्यावहारिक रूप से समर्पित हो जाना जिसे वह धारणा के रूप में अपना ईश्वर मान चुका है। इसी आज्ञापालन और समर्पण का नाम क़ुरआन की शब्दावली में ‘इस्लाम' हैं।
3-तीसरी मंजिल तकवा (ईशभय) की है जिसे साधारण भाषा मे कर्तव्यपरायण और उत्तरदायित्व की भावना से व्यक्त करते हैं। ईशभय यह है कि आदमी अपने जीवन के प्रत्येक पहलू मे यह समझते हुए कार्य करें कि उसे अपनी विचारधाराओं, कथनों और कर्मो का हिसाब ईश्वर को देना है। हर उस काम से रूक जाए जिससे ख़ुदा ने मना किया हैं, हर उस सेवा के लिए तत्पर हो जाए जिसका खुदा ने हुक्म दिया हैं और पूर्ण विवेकशील ढंग से वैध-अवैध, सही-ग़लत और भलाई-बुराई के बीच अन्तर करके जीवन व्यतीत करे।
अंतिम और उससे ऊंचा मंजिल ‘एहसान' (अति उत्तम आचरण) की है। एहसान का अर्थ यह हैं कि मनुष्य की इच्छा ईश्वर की इच्छा के साथ एकाकार हो जाए। जो कुछ ईश्वर की पासन्द है वही उसके दास की अपनी पसन्द भी हो और जो कुछ ईश्वर को नापसन्द है, दास का अपना दिल भी उसे नापसन्द करे। ईश्वर जिन बुराईयों को अपनी धरती पर देखना नहीं चाहता मनुष्य न केवल यह कि स्वयं उनसे बचे बल्कि उन्हे दुनिया से मिटा देने के लिए अपनी सम्पूर्ण क्षमताएं और सभी साधन लगा दे। ईश्वर जिन भलाईयों से अपनी धरती को सुसज्जित देखना चाहता है, मनुष्य उनको अपने जीवन में अपनाने तक ही सीमित न रहे बल्कि अपनी अपनी जान लड़ाकर दुनियाभर मे उन्हे फैलाने और स्थापित करने का प्रयास करे। इस स्थान पर पहुचकर मनुष्य को अपने ईश्वर का निकटतम सामीप्य प्राप्त होता हैं और इसी लिए यह इन्सान की आत्मिक उन्नति और विकास का उच्चतम शिखर है।
आध्यात्मिक उन्नति का यह रास्ता व्यक्तियों के लिए ही नही बल्कि वर्गो और समूहों के लिए भी है। एक व्यक्ति की भांति एक क़ौम (राष्ट्र) भी ईमान, आज्ञापालन और ईशभय की मंजिलों से गुजरकर एहसान की सर्वोच्च मंजिल तक पहुंच सकती है और एक राज्य भी अपनी पूर्ण व्यवस्था के साथ ईमानवाला, इस्लाम का अनुगामी, ईशभय धारण करनेवाला ओर एहसानवाला बन सकता हैं। बल्कि वास्तव में इस्लाम का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब एक पूरी क़ौम इसी मार्ग पर चले और दुनिया में एक ईशभय रखनेवाला उत्तम आचरण से सुसज्जित राज्य स्थापित हो जाए।
अब अध्यात्मिक प्रशिक्षण की उस व्यवस्था को भी देख लिया जाए जो व्यक्ति और समाज को इस रूप में तैयार करने के लिए इस्लाम ने पेश की हैं। इस व्यवस्था के चार स्तंभ हैं ।
(1) पहला स्तंभ नमाज़ है। यह प्रतिदिन पांच बार आदमी के मस्तिष्क में ख़ुदा की याद को ताजा करती है, उसका भय दिलाती है, उसका प्रेम पैदा करती हैं, उसके आदेश बार-बार सामने लाती है और आज्ञापालन का अभ्यास कराती है। यह नमाज़ केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि सामूहिकता के साथ अनिवार्य की गई ताकि पूरी सोसाइटी सामूहिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति के इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए।
(2) दूसरा स्तंभ रोज़ा है जो हर वर्ष पूरे माह तक मुसलमान व्यक्ति को अलग-अलग और मुस्लिम सोसाइटी को सामूहिक रूप से ईशभय का प्रशिक्षण देता रहता है।
(3) तीसरा स्तंभ ज़कात है जो मुसलमान व्यक्तियों में आर्थिक त्याग भाव, आपसी हमदर्दी और मदद की भावना उत्पन्न करती है। आजकल के लोग भ्रमवश ज़कात को कर (Tax) के अर्थ मे लेते हैं, जबकि ‘ज़कात' की आत्मा कर की आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ज़कात का मूल शाब्दिक अर्थ वृद्धि विकास और शुद्धता है। इस शब्द से इस्लाम आदमी के मन मे यह तथ्य बैठाना चाहता है कि अल्लाह की मुहब्बत में अपने भाइयों की तुम जो आर्थिक सहायता करोगे, इससे तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा और तुम्हारे आचरण में पवित्रता और शुद्धता आएगी।
(4) चौथा स्तंभ हज हैं यह ईशभक्ति की धुरी पर ईमानवाले और आस्थावान मनुष्यों की एक अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी बनाता है और एक ऐसा विश्वव्यापी आन्दोलन चलाता है जो दुनिया में सदियों से ‘सत्य' के आहवान पर एक जुटता का ऐलान कर रही है और ईश्वर ने चाहा तो रहती दुनिया तक वह ऐलान करता रहेगा।
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
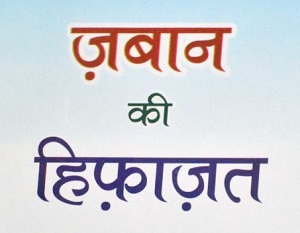
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
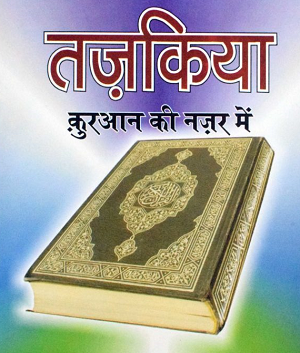
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

