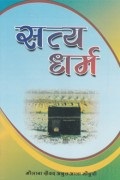
सत्य धर्म
-
इस्लाम
- at 21 March 2020
मानव-जीवन एक ऐसी इकाई है, जिसे अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न विभागों में तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तव में वे सारे विभाग एक ही सिद्धांत और नियम का पालन करते हैं। अतः मानव के सम्पूर्ण जीवन का एक ही धर्म होना चाहिए। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग धर्मों का पालन या अलग-अलग नियमों का अनुसरण विश्वास के अस्थिर और बौद्धिक-निर्णय के विचलित होने का प्रमाण है। जब किसी धर्म के सत्य धर्म होने का पूरा विश्वास प्राप्त हो तो जीवन के समस्त विभागों में उसका अनिवार्यतः पालन होना चाहिए और केवल उसी को समस्त जीवन का धर्म होना चाहिए। -संपादक
मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी
यह भाषण 21 मार्च 1943 ई0 को जामिआ मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में दिया गया था।
(मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी (1903-1979) वर्तमान युग में इस्लाम के मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे अपने समय के एक महान इस्लामी विचारक और लेखक थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन युगापेक्षित इस्लाम की व्याख्या करने और उसके सन्देश को आम करने तथा इस्लामी जीवन-व्यवस्था क़ायम करने की कोशिश में लगा दिया। इस जिददो-जुहद में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन् 1941 में उन्होंने ‘जमाअत इस्लामी' की स्थापना की जिसके वे 1972 ई0 तक आमीर (अध्यक्ष) रहे, जो कि वर्तमान युग का एक महत्वपूर्ण इस्लामी संगठन है। 1942 से 1967 ई0 तक की अवधि में उन्हें चार बार जेल जाना पड़ा, जहाँ पाकिस्तान की अनेक जेलों में पाँच वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1953 ई0 में तो उनकी एक पुस्तक को आधार बना कर फ़ौजी अदालत ने उन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गयी। मौलाना मौदूदी ने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखीं जो ज्ञानवर्धक और अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुईं। उन की पुस्तकों का देश-विदेश की 40 भाषाओं में रूपांतरण हो चुका है। )
‘‘अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है।''
क़ुरआन जिस दावे के साथ मानव-जाति को अपने प्रस्तुत किए हुए मार्ग की ओर बुलाता है वह स्वयं उसके अपने शब्दों में यह है-
इन्नद् दी-न इन्दल्लाहिल इस्लाम (क़ुरआन-3:19)
यही छोटा-सा वाक्य इस समय मेरे विवेचन का विषय है। अधिक विस्तार का अवसर नहीं, अत्यंत संक्षेप में मैं पहले इसके अर्थ की व्याख्या करूंगा। जिससे स्पष्ट हो जाएगा। कि इस वाक्य में वास्तव में किस बात का दावा किया गया है। फिर इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि यह दावा स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, और अन्त में मैं यह बयान करूंगा कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो फिर इसे स्वीकार कर लेने के तक़ाज़े (दायित्व) क्या हैं ?
साधारणतया इस वाक्य का जो सीधा-सादा अर्थ बयान किया जाता है वह यह है कि ‘‘सत्यधर्म तो ईश्वर के निकट केवल इस्लाम है।'' और ‘इस्लाम' की जो धारणा साधारणतः लोगों के मस्तिष्क में है वह इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि यह एक धर्म का नाम है, जिसने अब से तेरह सौ वर्ष पहले अरब में जन्म लिया था और जिसकी स्थापना हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने की थी। ‘‘स्थापना की थी'' का शब्द में जान-बूझ कर इस लिए प्रयोग कर रहा हूँ कि केवल ग़ैर-मुस्लिम ही नहीं बल्कि बहुत-से मुसलमान और अच्छे-ख़ासे विद्वान मुसलमान भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) को ‘‘इस्लाम का संस्थापक'' कहते और लिखते हैं। मानो उनके निकट इस्लाम का आरम्भ हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) के द्वारा ही हुआ है और आप ही उसके संस्थापक (Founder) हैं। अतः जब एक ग़ैर-मुस्लिम क़ुरआन का अध्ययन करते हुए इस वाक्य पर पहुँचता है तो वह यह सोच कर सरसरी तौर पर उस स्थान से गुज़र जाता है कि जिस प्रकार प्रत्येक धर्म केवल अपने ही सत्य होने और दूसरे धर्मों के असत्य होने का दावेदार है, उसी प्रकार क़ुरआन ने भी अपने प्रस्तुत किए हुए धर्म के सत्य होने का दावा कर दिया है; और जब एक मुसलमान उसे पढ़ता है तो वह इसलिए इस पर विचार करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझता कि जिस धर्म को इस वाक्य में सत्य कहा गया है उसे वह स्वयं भी सत्य मानता है या यदि सोच-विचार के लिए उसके मस्तिष्क में कोई प्रेरणा उत्पन्न भी होती है तो वह साधारणतः यह रूप ग्रहण कर लेती है कि ईसाइयत, हिन्दूधर्म, बौद्धमत और ऐसे ही दूसरे धर्मों से इस्लाम की तुलना करके उसकी सत्यता प्रमाणित की जाए। किन्तु, वास्तव में क़ुरआन में यह स्थान ऐसा है जिस पर एक गम्भीर विद्यार्थी को रुक कर बहुत विचार और चिन्तन करना चाहिए। उससे अधिक विचार करना चाहिए जितना अब तक इस पर विचार किया गया है।
क़ुरआन के इस दावे को समझने के लिए सबसे पहले हमें ‘‘अद्-दीन''और ‘‘अल-इस्लाम'', का अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए।
‘अद्-दीन' का अर्थ
अरबी भाषा में ‘दीन' शब्द कई अर्थो में आता है, उसका एक अर्थ सत्ता और संप्रभुत्व है, दूसरा अर्थ दासता और आज्ञापालन, तीसरा अर्थ बदला और पुरस्कार, चैथा अर्थ मार्ग और प्रणाली है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसी चौथे अर्थ में हुआ है। अर्थात् दीन का अभिप्राय जीवन-प्रणाली या विचार एवं आचरण की वह पद्धति है जिसका पालन किया जाए।
लेकिन यह याद रहे कि क़ुरआन केवल ‘‘दीन'' नहीं कह रहा है बल्कि ‘‘अद-दीन'' कह रहा है। इससे अर्थ में वही अन्तर पड़ जाता है जो अंग्रेजी भाषा में This is a way कहने के स्थान पर This is the way कहने से पड़ता है। अर्थात क़ुरआन का दावा यह नहीं है कि ईश्वर के निकट इस्लाम एक जीवन-प्रणाली है, बल्कि उसका दावा यह है कि इस्लाम ही एक सत्य और वास्तविक जीवन प्रणाली या विचार-शैली अथवा आचरण-पद्धति है।
फिर यह बात भी ध्यान में रहे कि क़ुरआन इस शब्द का प्रयोग किसी सीमित अर्थ में नहीं अपितु अधिक व्यापक अर्थ में करता है। जीवन-प्रणाली से उसका तात्पर्य जीवन के किसी विशेष पहलू या किसी विशेष विभाग की प्रणाली नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन की प्रणाली है। अलग-अलग एक-एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन ही की प्रणाली नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से पूरे समाज की जीवन-प्रणाली भी है। एक देश विदेश या एक राष्ट्र विशेष या काल विशेष की जीवन-प्रणाली नहीं, बल्कि समस्त कालों में, समस्त मनुष्यों की व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन-प्रणाली है। अतः क़ुरआन के दावे का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर के निकट पूजा-पाठ और परलोक के विश्वास और मुत्यु के पश्चात जीवन की धारणा का एक यथार्थ संग्रह वही है जिसका नाम इस्लाम है, और न उसका अर्थ यह है कि समस्त मनुष्यों के धार्मिक विचार और कर्म की नीति (जैसा कि ‘‘धार्मिक'' शब्द का आज कल की पश्चिमी परिभाषा में लिया जाता है) का एक वास्तविक रूप वही है जिसे इस्लाम कहा गया है; न उसका अर्थ यह है कि अरब के लोगों या अमुक शताब्दी तक के मनुष्यों या अमुक युग उदाहरणतः औद्योगिक क्रान्ति से पहले तक के मनुष्यों के लिए एक वास्तविक जीवन-व्यवस्था वही है जिसको इस्लाम का नाम दिया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से उसका दावा यह है कि हर काल और हर युग में समस्त मनुष्यों के लिए धरती पर जीवन व्यतीत करने का एक ही ढंग ईश्वर के निकट ठीक है और वह ढंग वही है जिसका नाम ‘‘अल-इस्लाम'' है।
मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एशिया और यूरोप के बीच किसी स्थान पर क़ुरआन की कोई नई टीका की गई है, जिसके अनुसार ‘‘दीन'' का अर्थ केवल मनुष्य और ईश्वर के व्यक्तिगत सम्बन्ध तक सीमित है और संस्कृति एवं राजनीति की व्यवस्था से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह टीका यदि स्वयं क़ुरआन से प्राप्त की गई है तो अवश्य बड़ी मनोरंजक वस्तु होगी, परन्तु मैंने अट्ठारह वर्ष तक क़ुरआन का जो शोधपरक गहन अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि क़ुरआन अपने समस्त आधुनिक भाष्यकारों की इव्छाओं के विरुद्ध ‘‘अद्-दीन'' को शब्द का किसी सीमित अर्थ में प्रयोग नहीं करता बल्कि समस्त युगों के समस्त मनुष्यों के लिए उनके सम्पूर्ण जीवन की विचार एवं आचरण की व्यवस्था के अर्थ में प्रयोग करता है।
‘अल-इस्लाम' का अर्थ
अब ‘‘इस्लाम'' शब्द को लीजिए। अरबी भाषा में इसके अर्थ हैं हथियार डाल देना, झुक जाना, आज्ञा-पालन स्वीकार कर लेना, अपने आपको समर्पित कर देना। किन्तु क़ुरआन केवल ‘इस्लाम' नहीं बोलता, बल्कि ‘‘अल-इस्लाम'' बोलता है, जो उसका विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। इस विशिष्ट पारिभाष्कि शब्द से उसका तात्पर्य ईश्वर के आगे झुक जाना, उसका आज्ञा-पालन स्वीकार कर लेना, उसके सम्मुख अपनी स्वतन्त्रता से अधिकार रहित हो जाना और अपने आपको उसको समर्पित कर देना है। इस स्वीकृति, आज्ञा-पालन, और समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि प्राकृतिक-नियमों के आगे हथियार डाल दिया जाए जैसा कि कुछ लोगों ने इसका अर्थ निश्चित करने की चेष्टा की है, न इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कल्पना या अपने निरीक्षणों और अनुभवों से ईश्वर की प्रसन्नता और उसकी इच्छा की जो धारणा अपने-आप ग्रहण कर ले उसी का आज्ञा-पालन करने लगे, जैसा कि कुछ और लोगों ने अपनी भूल से समझ लिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने स्वयं अपने सन्देष्टा (रसूलों) द्वारा मनुष्य के लिए जिस विचार प्रणाली और कर्म-नीति की ओर पथ-प्रदर्शन किया है, उसको वह स्वीकार कर ले और अपने विचार तथा आचरण की स्वतन्त्रता या उचिततर शब्दों में विचार तथा आचरण की उच्छृंखलता छोड़ कर उसकी आज्ञा का पालन और उसका अनुसरण ग्रहण कर ले। इसी वस्तु को क़ुरआन ‘‘अल-इस्लाम'' कहता है। और यह वास्तव में कोई नवयुगीन धर्म नहीं है जिसकी स्थापना अब से 1333 वर्ष पहले अरब में हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) (उन पर ईश्वर की दया और कृपा हो) ने की बल्कि जिस दिन पहली बार इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रकट हुआ उसी दिन ईश्वर ने मुनष्य को बता दिया था कि तेरे लिए केवल ‘‘अल-इस्लाम'' ही एक वास्तविक कार्य-प्रणाली है। और उसके बाद संसार के विभिन्न भागों में समय-समय पर जो सन्देष्टा (रसूल) भी ईश्वर की ओर से मनुष्यों के पथ-प्रदर्शन के लिए नियुक्त हुए हैं उन सबका बुलावा भी समान रूप से इसी ‘‘अल-इस्लाम'' की ओर रहा है जिसकी ओर अन्ततः हज़रत मुहम्मद (उन पर ईश्वर की दया-कृपा हो) ने संसार को निमन्त्रण दिया। यह और बात है कि मूसा (उन पर ईश्वर की सलामती हो) के अनुयायियों ने बाद में बहुत-सी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का सम्मिश्रण करके एक धर्म-व्यवस्था ‘यहूदियत' के नाम से और ईसा (उन पर ईश्वर की अनुकम्पा हो) के अनुयायियों ने एक दूसरी धर्म-व्यवस्था ‘ईसाइसत' के नाम से, और इसी प्रकार भारत, ईरान, चीन और दूसरे देशों के सन्देष्टाओं (पैग़म्बरों) के अनुयायियों ने विभिन्न प्रकार की मिली-जुली व्यवस्थाएँ बना ली हों, किन्तु मूसा और ईसा और दूसरे समस्त प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध पैग़म्बर एवं ईश-दूत जिस धर्म का बुलावा देने आए वह केवल विशुद्ध इस्लाम था न कि कुछ और।
क़ुरआन का दावा क्या है ?
इस व्याख्या के बाद क़ुरआन का दावा प्रकट और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है और वह यह है-
‘‘मुनष्य-जाति के लिए ईश्वर के निकट केवल यह एक ठीक जीवन-प्रणाली है कि वह ईश्वर की आज्ञाओं के आगे नत-मस्तक हो जाए और विचार और कार्य के उस मार्ग पर चले जिसकी ओर ईश्वर ने अपने पैग़म्बरों द्वारा पथ-प्रदर्शन किया है!''
यह है क़ुरआन का दावा। अब हमें इसकी विवेचना करनी है कि क्या यह दावा स्वीकार किया जाना चाहिए ? स्वयं क़ुरआन ने अपने इस दावे के समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किए है उन पर तो हम विचार करेंगे ही किन्तु क्यों न इससे पहले स्वयं अपनी जगह समीक्षा एवं अन्वेषण द्वारा यह मालूम कर लें कि क्या हमारे लिए इस दावे को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और उपाय भी है?
‘जीवन-प्रणाली' की आवश्यकता
यह विदित है कि संसार में मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए हर स्थिति में एक जीवन-प्रणाली आवश्यक है जिसे वह ग्रहण करे। मनुष्य नदी नहीं है जिसका मार्ग पृथ्वी की ऊॅंचाई-नीचाई से स्वयं निश्चित हो जाता है, मनुष्य वृक्ष नहीं है जिसके लिए प्राकृतिक नियम एक मार्ग निश्चित कर देते हैं, मनुष्य निरा पशु भी नहीं है जिसके पथ-प्रदर्शन के लिए केवल प्रकृति पर्याप्त हो जाती है। अपने जीवन के एक बड़े भाग में प्राकृतिक नियमों का दास होते हुए भी मनुष्य जीवन के बहुत-से ऐसे पहलू रखता है जिसमें उसे कोई लगा-बंधा मार्ग नहीं मिलता कि पशुओं के समान विवश रूप से उस पर चलता रहे, बल्कि उसको अपनी इच्छा से ख़ुद एक मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। उसको विचार का एक मार्ग चाहिए जिस पर चलकर वह अपनी और सृष्टि की उन बहुत-सी समस्याओं को हल कर सके, जिन्हें प्रकृति उसके सोचने वाले दिमाग़ के सामने प्रस्तुत करती है, किन्तु उनका कोई हल वह स्पष्ट और सन्देह-रहित भाषा में नहीं बताती। उसको ज्ञान का एक रास्ता चाहिए; जिस पर चलकर या जिसका अनुसरण कर वह उन जानकारियों को संगठित कर सके जिन्हें प्रकृति उसकी इन्द्रियों द्वारा उसके मस्तिष्क तक पहुँचाती है, किन्तु उन्हें स्वयं अपने ढंग से संगठित करके उनको सौंप नहीं देती। उसको व्यक्तिगत व्यवहार के लिए एक मार्ग चाहिए जिस पर वह अपने अस्तित्व की बहुत-सी उन माँगो को पूरा करे जिनके लिए प्रकृति तक़ाज़ा तो करती है किन्तु उन्हें पूरा करने की कोई सभ्य-प्रणाली निश्चित करके नहीं देती। उसको घरेलू जीवन के लिए, पारिवारिक सम्बन्धों के लिए, जीविका सम्बन्धी व्यवहारों के लिए, राष्ट्र-व्यवस्था के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के लिए और जीवन के बहुत-से दूसरे पहलुओं के लिए भी एक मार्ग चाहिए जिस पर वह केवल एक व्यक्ति ही की हैसियत से नहीं, बल्कि एक समाज, एक राष्ट्र, एक जाति के रूप में भी अग्रसर हो और उन उद्देश्यों तक पहुँच सके जो यद्यपि स्वभावतः उसके उद्देश्य और अभिप्राय हैं, किन्तु प्रकृति ने न तो उन उद्देश्यों को खुले तौर पर उसके सामने प्रकट किया है और न उन तक पहुँचने का एक मार्ग निश्चित कर दिया है।
जीवन अविभाज्य है
जीवन के ये विभिन्न पहलू जिसमें कोई एक ढंग ग्रहण करना मुनष्य के लिए अनिवार्य है अपने स्थान पर स्वयं स्थायी औेर एक-दूसरे से असम्बद्ध विभाग व महकमे नहीं हैं कि उनमें से प्रत्येक के लिए मुनष्य अलग-अलग मार्ग ग्रहण कर सकता हो जिनकी दिशाएँ अलग हों, जिनकी मार्ग-सामग्रियाँ अलग हों, जिन पर चलने के ढंग और प्रणालियाँ अलग हों, जिनकी यात्रा के उद्देश्य अलग हों और जिसके यात्रा लक्ष्य अलग हों। मनुष्य और उसके जीवन की समस्याओं को समझने की एक तनिक-सी बुद्धि-युक्त चेष्टा ही मनुष्य को इस बात पर संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि जीवन सामूहिक रूप से एक सर्वस्व है, जिसका हर भाग दूसरे भाग से और हर पहलू दूसरे पहलू से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। हर एक दूसरे पर प्रभाव डालता है, एक ही आत्मा सब में प्रविष्ट किए हुए होती है और सब मिलकर वह चीज़ बनाते हैं जिसे मानव-जीवन कहा जाता है। अतः वास्तव में जो वस्तु मनुष्य के लिए आवश्यक है वह जीवन के बहुत-से उद्देश्य नहीं हैं, बल्कि एक उद्देश्य है जिसके अन्तर्गत सारे छोटे-बड़े उद्देश्य पूर्ण सहयोग के साथ अपने-अपने स्थान ग्रहण कर सकें और जिसकी प्राप्ति की चेष्टा में वह समस्त उद्देश्य प्राप्त हो जाएँ। उसको मार्गों की नहीं बल्कि केवल एक मार्ग ही आवश्यकता है जिस पर वह अपने समस्त जीवन को उसके समस्त पहलुओं समेत पूरी समरता के साथ अपने जीवन लक्ष्य की ओर ले चले। उसको विचार, ज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, धर्म, नीति, समाज, जीविका, राजनीति, विधान आदि के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ नहीं बल्कि एक पूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें यह सब समरसता के साथ समोये जा सकें जिसमें उन सबके लिए एक ही स्वभाव और एक ही गुण रखने वाले उचित नियम मौजूद हों और जिसका अनुसरण करके मनुष्य और मनुष्यों का हर समूह और सर्वस्वरूप से सारी मनुष्यता अपने उच्चतर लक्ष्य तक पहुँच सके। वह अज्ञानता का अन्धकारमय युग था, जब जीवन को स्थायी रूप से विभिन्न विभागों में विभाजित करना सम्भव समझा जाता था।
अब यदि कुछ लोग इस विचार शैली के व्यर्थ वार्तालाप करने वाले मौजूद हैं तो वे बेचारे या तो ख़ुलूस के साथ पुराने विचारों के वातावरण में अब तक सांस ले रहे हैं इसलिए दया के पात्र हैं या फिर वे अत्याचारी हैं जो सत्यता को भली-भांति जानते हैं किन्तु जान बूझकर ऐसी बात सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि जिस ‘‘धर्म'' को वे किसी मानव-समाज में फैलाना चाहते हैं; उसके नियमों से असहमति रखने वालों को उन्हें यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे इस धर्म के अन्तर्गत तुम्हें जीवन के अमुक-अमुक विभागों में, जो दुर्भाग्य से तुमको अत्यन्त प्रिय हैं, पूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहेगी। हालाँकि यह सुरक्षा ज्ञान की दृष्टि से असम्भव, प्राकृतिक दृष्टि से निषिद्ध और व्यवहारतः असम्भव है। और इस प्रकार की बातें करने वाले सम्भवतः स्वयं भी जानते हैं कि यह असम्भव है। हर प्रभुत्व-प्राप्त धर्म, जीवन के समस्त विभागों को अपनी आत्मा और अपने स्वभाव के अनुसार ढाल कर ही रहता है जिस प्रकार हर नमक की खान उन समस्त वस्तुओं को नमक में बदल करके ही रहती है जो उसकी सीमा में प्रविष्ट हो जाएँ।
जीवन का भौगोलिक वंशागत विभाजन
फिर जिस प्रकार यह बात व्यर्थ है कि मानव-जीवन को भिन्न-भिन्न विभागों में विभाजित किया जाए उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक व्यर्थ बात यह है कि उसे भौगोलिक क्षेत्रों या वंशगत परिधियों में विभाजित किया जाए। मनुष्य निःसन्देह पृथ्वी के बहुत-से भागों में पाया जाता है जिनको नदियों ने, पहाड़ों ने, वनों और सागरों ने या कृतिम सीमाओं ने विभक्त कर रखा है और मुनष्य की बहुत-सी भिन्न-भिन्न नस्लें और जातियाँ भी अवश्य पाई जाती हैं, जिनके बीच ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और दूसरे कारणों से मनुष्यता के विकास और उन्नति ने विभिन्न रूप ग्रहण किए हैं, किन्तु इस विभिन्नता को दलील ठहरा कर जो व्यक्ति यह कहता है कि हर जाति, हर राष्ट्र और हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए ‘धर्म' अर्थात् जीवन-व्यवस्था अलग होनी चाहिए वह सरासर एक व्यर्थ बात करता है। उसकी सीमित दृष्टि बाह्य दृश्यों और बाह्य अवस्थाओं की विभिन्नताओं में उलझ कर रह गई, इस बाहरी विविधता के अन्दर सूक्ष्म मानवीय गुण-धर्म की एकता को वह नहीं पा सका। यदि वास्तव में ये विभिन्नताएँ इतनी महत्व रखती हैं कि उन के आधार पर धर्म अलग-अलग होने चाहिएँ तो मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक जो विभिन्नताएँ एक देश और दूसरे देश, एक वंश और दूसरे वंश के बीच आप पाते हैं उन सब को जितना बढ़ा-चढ़ा कर चाहें लिख लें और फिर उन विभिन्नताओं का शुद्ध वैज्ञानिक विवेचन करें जो स्त्री और पुरुष में पाई जाती हैं, जो हर मनुष्य और दूसरे मनुष्य में पाई जाती हैं, जो एक ही माता और पिता के दो बच्चों में पाई जाती हैं तो कदाचित अत्युक्ति न होगी यदि मैं यह दावा करूं कि ज्ञानात्मक तर्क और विश्लेषण में प्रथम की विभिन्नताओं से ये दूसरी प्रकार की विभिन्नताएँ हर अवस्था में प्रबल ही निकलेंगी, फिर क्यों न कह दीजिए कि हर व्यक्ति की जीवन-व्यवस्था अलग होनी चाहिए ? किन्तु जब आप व्यक्तिगत, जातीय और पारिवारिक बाहुल्य के बीच एकता का एक तत्व और स्थायी तत्व ऐसा पाते हैं जिसके आधार पर एक राष्ट्र या एक देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए एक जीवन-व्यवस्था होना सम्भव समझा जाता है, तो आख़िर किस वस्तु ने आप को रोक दिया है कि राष्ट्रीय, जातीय, मातृभूमि की विविधता के बीच एक और बड़ी आधारात्मक एकता का तत्व आप नहीं पा सकते, जिस पर मानवता की धारणा स्थित हो और जिस के आधार पर समस्त मानव-संसार का एक धर्म या जीवन -व्यवस्था होना सम्भव समझा जाए ? क्या यह वस्तविकता नहीं है कि समस्त भौगोलिक, वांशिक और राष्ट्रीय विभिन्नताओं के होते हुए भी वे प्राकृतिक नियम समान हैं, जिनके अन्तर्गत मुनष्य संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है। वह शारीरिक व्यवस्था समान है जिसके अनुसार मनुष्य की रचना की गई है, वे गुण समान हैं, जिनके आधार पर मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग एक स्थायी जाति ठहरता है, वे प्राकृतिक मांगें और आवश्यकताएँ समान हैं जो मनुष्य के अन्तःकरण में निहित की गई हैं, वह शक्तियाँ समान हैं जिनके समूह को हम मानव वृत्ति कहते हैं और आधार भूत रूप से वे समस्त प्राकृतिक, मानसिक ऐतिहासिक, संस्कृतिक, जीविका सम्बन्धी कारक भी समान हैं जो मानव जीवन में कार्यशील हैं ? यदि यह सत्य है- और कौन कह सकता है कि यह सत्य नहीं है-तो जो सिद्धान्त मनुष्य के कल्याण के लिए ठीक हों उनको विश्वव्यापी होना चाहिए, उनके जातिपरक या वंशपरक या देशपरक होने का कोई कारण नहीं। राष्ट्र और जातियाँ इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन और आंशिक रूप से अपने जीवन सम्बन्धी व्यवहारों का प्रबन्ध विभिन्न रीतियों से कर सकती हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। किन्तु मनुष्य को मनुष्य होने की दृष्टि से जिस वास्तविक धर्म या जीवन-व्यवस्था की आवश्यकता है वह हर स्थिति में एक ही होनी चाहिए। बुद्धि यह स्वीकार करने से इनकार करती है कि जो वस्तु एक राष्ट्र के लिए सत्य हो वह दूसरे राष्ट्र के लिए असत्य हो जाए और जो एक राष्ट्र के लिए असत्य हो वह दूसरे के लिए सत्य हो जाए।
जीवन का सामयिक विभाजन
इन निरर्थकताओं और आधुनिक काल की ज्ञानात्मक निरर्थकताओं में से एक और बात जो वास्तविकता की दृष्टि से अत्यधिक निरर्थक है, किन्तु आश्चर्य है कि विश्वास की पूरी शक्ति के साथ प्रस्तुत की जाती है, मानव-जीवन का सामयिक विभाजन है अर्थात कहा जाता है कि जो जीवन-व्यवस्था एक युग में सत्य होती है वह दूसरे युग में असत्य हो जाती है। क्योंकि जीवन की समस्याएँ और प्रसंग हर काल में बदल जाते हैं और जीवन-व्यवस्था का सत्य या असत्य होना सरासर उन समस्याओं और प्रसंगों ही की स्थिति पर निर्भर है। यह बात उसी मानव-जीवन के सम्बन्ध में कही जाती है जिसके बारे में साथ ही साथ विकास की बात भी की जाती है। जिसके इतिहास में क्रियाशील नियम भी ढूंढ़े जाते हैं, जिसके पिछले अनुभवों से वर्तमान के लिए शिक्षा और भविष्य के लिए आदेश भी निर्गत किए जाते हैं और जिसके लिए ‘‘मानव प्रकृति'' नाम की एक वस्तु भी प्रमाणित की जाती है। मैं पूछता हूँ क्या आपके पास कोई ऐसा मापक-यन्त्र है जिससे आप मान-जाति की इस निरन्तर ऐतिहासिक गति के बीच काल या युग या समय की वास्तविक सीमाबन्दियाँ कर सकते हों ? और क्या यह सम्भव है कि इन सीमाबन्दियों में से किसी एक रेखा पर उंगली रखकर आप कह सकते हों कि इस रेखा के उस पार जो जीवन-समस्याएँ थीं वे इस पार आकर बिलकुल बदल गईं; और जो परिस्थियाँ उस पार थीं, वे इस पार बाक़ी नहीं ? यदि वास्तव में मानव-इतिहास ऐसे ही अलग-अलग सामयिक भागों में विभाजित है तब तो यूं समझना चाहिए कि एक भाग जो समाप्त हो चुका है वह बाद वाले भागों के लिए केवल एक निरर्थक और व्यर्थ वस्तु हो गई। उसके समाप्त होते ही वह सब कुछ नष्ट हो गया जो मनुष्य ने काल के उस भाग में किया था। उस काल में मनुष्य को जो अनुभव प्राप्त हुए वह बाद वाले काल के लिए अपने अन्दर कोई शिक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे परिस्थितियाँ और वे समस्याएँ ही लुप्त हो गईं जिनमें मनुष्य ने कुछ प्रणालियों या कुछ नियमों का कुछ मूल्यों के लिए प्रयास और चेष्टा का प्रयोग किया था। फिर यह विकास की वार्ता क्यों ? यह जीवन-नियम का अन्वेषण किस लिए ? यह ऐतिहासिक निष्कर्ष किस आधार पर ? जब आप विकास का नाम लेते हैं तो अनिवार्यतः यह इस बात का प्रमाण है कि वहाँ अवश्य कोई वस्तु है जो समस्त परिवर्तनों का विषय बनती है और उन परिवर्तनों के भीतर अपने आपको स्थिर रखते हुए निरन्तर गतिशील है। जब आप जीवन-विधि पर विवाद करते हैं तो यह बात वांछनीय है कि इन अस्थिर परिस्थितियों में इन चलते-फिरते दृश्यों में, इन बनने और बिगड़ने वाली सूरतों में कोई स्थायी और जीवित तथ्य भी है जो अपनी एक विशेष प्रकृति और अपने कुछ स्थायी नियम भी रखती है। जब आप इतिहास से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि इतिहास के इस सुदीर्घ मार्ग पर जो यात्री विभिन्न स्थानों से गुज़रता हुआ आ रहा है, और मंज़िलों पर मंज़िले तय करता हुआ चला आ रहा है, वह स्वयं अपना कोई व्यक्त्त्वि और अपना कोई स्थायी स्वभाव रखता है, जिसके सम्बन्ध में यह आज्ञा लागू की जा सकती है कि वह विशेष परिस्थिति में विशेष रूप से कार्य करता है। वह एक समय में कुछ वस्तुओं को स्वीकार करता है और दूसरे समय में उन्हें अस्वीकार कर देता है और कुछ दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। यह जीवित सत्य, यह स्थायी विषय-परिवर्तन, यह इतिहास के राज-पथ का स्थायी पथिक ही तो है जिसे आप सम्भवतः ‘‘मानवता'' कहते हैं। किन्तु क्या बात है कि जब आप रास्ते की मंज़िलों और उनमें पेश आने वाली परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर वार्तालाप आरम्भ करते हैं तो इस वार्तालाप में ऐसे खो जाते हैं कि स्वयं यात्री आपको याद नहीं रहता ? क्या यह सच है कि मंज़िलें और उनकी परिस्थितियाँ और उनकी समस्याएँ बदल जाने से यात्री और उसी वास्तविकता भी बदल जाती है ? हम तो यह देखते हैं कि आदि सृष्टि से आज तक उसकी बनावट बिल्कुल नहीं बदली, उसके विधितत्व वही हैं जो अब से हज़ारों वर्ष पहले थे, उसका स्वभाव वही है, उसकी प्रकृति की मांगे वही है, उसके गुण और उसकी विशेषताएँ वही हैं, उसकी रूचियाँ और उसकी इच्छाएँ वही हैं उसकी शक्तियाँ और उसकी योग्यताएँ वही हैं, उसकी दुर्बलताएँ और अयोग्यताएँ वही हैं, उसके कार्य करने और कार्य-प्रभाव स्वीकार करने और प्रभावित होने के नियम वही हैं, उस पर शासन करने वाली शक्तियाँ वही हैं, और उसका चतुर्दिक विश्व-वातावरण भी वही है। उनमें से किसी वस्तु में भी आदि सृष्टि से आज तक कण मात्र भी अन्तर नहीं आया है। कोई व्यक्ति यह दावा करने का साहस नहीं कर सकता कि इतिहास के बीच में परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न होने वाली जीवन समस्याओं के परिवर्तन से स्वयं मानवता भी परिवर्तित होती आई है। या वे बुनियादी वस्तुएँ भी परिवर्तित होती रही हैं जो मानवता से सम्बन्ध रखती हैं। फिर जब वास्तविकता यह है तो इस दावे में क्या वज़न हो सकता है कि मनुष्य के लिए जो वस्तु कल अमृत थी वह आज विष है, जो वस्तु कल सत्य थी वह आज असत्य है, जो वस्तु कल मूल्य रखती थी वह आज मूल्यहीन है।
जीवन अविभाज्य है
जीवन के ये विभिन्न पहलू जिसमें कोई एक ढंग ग्रहण करना मुनष्य के लिए अनिवार्य है अपने स्थान पर स्वयं स्थायी औेर एक-दूसरे से असम्बद्ध विभाग व महकमे नहीं हैं कि उनमें से प्रत्येक के लिए मुनष्य अलग-अलग मार्ग ग्रहण कर सकता हो जिनकी दिशाएँ अलग हों, जिनकी मार्ग-सामग्रियाँ अलग हों, जिन पर चलने के ढंग और प्रणालियाँ अलग हों, जिनकी यात्रा के उद्देश्य अलग हों और जिसके यात्रा लक्ष्य अलग हों। मनुष्य और उसके जीवन की समस्याओं को समझने की एक तनिक-सी बुद्धि-युक्त चेष्टा ही मनुष्य को इस बात पर संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि जीवन सामूहिक रूप से एक सर्वस्व है, जिसका हर भाग दूसरे भाग से और हर पहलू दूसरे पहलू से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है जो तोड़ा नहीं जा सकता। हर एक दूसरे पर प्रभाव डालता है, एक ही आत्मा सब में प्रविष्ट किए हुए होती है और सब मिलकर वह चीज़ बनाते हैं जिसे मानव-जीवन कहा जाता है। अतः वास्तव में जो वस्तु मनुष्य के लिए आवश्यक है वह जीवन के बहुत-से उद्देश्य नहीं हैं, बल्कि एक उद्देश्य है जिसके अन्तर्गत सारे छोटे-बड़े उद्देश्य पूर्ण सहयोग के साथ अपने-अपने स्थान ग्रहण कर सकें और जिसकी प्राप्ति की चेष्टा में वह समस्त उद्देश्य प्राप्त हो जाएँ। उसको मार्गों की नहीं बल्कि केवल एक मार्ग ही आवश्यकता है जिस पर वह अपने समस्त जीवन को उसके समस्त पहलुओं समेत पूरी समरता के साथ अपने जीवन लक्ष्य की ओर ले चले। उसको विचार, ज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, धर्म, नीति, समाज, जीविका, राजनीति, विधान आदि के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ नहीं बल्कि एक पूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें यह सब समरसता के साथ समोये जा सकें जिसमें उन सबके लिए एक ही स्वभाव और एक ही गुण रखने वाले उचित नियम मौजूद हों और जिसका अनुसरण करके मनुष्य और मनुष्यों का हर समूह और सर्वस्वरूप से सारी मनुष्यता अपने उच्चतर लक्ष्य तक पहुँच सके। वह अज्ञानता का अन्धकारमय युग था, जब जीवन को स्थायी रूप से विभिन्न विभागों में विभाजित करना सम्भव समझा जाता था।
अब यदि कुछ लोग इस विचार शैली के व्यर्थ वार्तालाप करने वाले मौजूद हैं तो वे बेचारे या तो ख़ुलूस के साथ पुराने विचारों के वातावरण में अब तक सांस ले रहे हैं इसलिए दया के पात्र हैं या फिर वे अत्याचारी हैं जो सत्यता को भली-भांति जानते हैं किन्तु जान बूझकर ऐसी बात सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि जिस ‘‘धर्म'' को वे किसी मानव-समाज में फैलाना चाहते हैं; उसके नियमों से असहमति रखने वालों को उन्हें यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे इस धर्म के अन्तर्गत तुम्हें जीवन के अमुक-अमुक विभागों में, जो दुर्भाग्य से तुमको अत्यन्त प्रिय हैं, पूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहेगी। हालाँकि यह सुरक्षा ज्ञान की दृष्टि से असम्भव, प्राकृतिक दृष्टि से निषिद्ध और व्यवहारतः असम्भव है। और इस प्रकार की बातें करने वाले सम्भवतः स्वयं भी जानते हैं कि यह असम्भव है। हर प्रभुत्व-प्राप्त धर्म, जीवन के समस्त विभागों को अपनी आत्मा और अपने स्वभाव के अनुसार ढाल कर ही रहता है जिस प्रकार हर नमक की खान उन समस्त वस्तुओं को नमक में बदल करके ही रहती है जो उसकी सीमा में प्रविष्ट हो जाएँ।
जीवन का भौगोलिक वंशागत विभाजन
फिर जिस प्रकार यह बात व्यर्थ है कि मानव-जीवन को भिन्न-भिन्न विभागों में विभाजित किया जाए उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक व्यर्थ बात यह है कि उसे भौगोलिक क्षेत्रों या वंशगत परिधियों में विभाजित किया जाए। मनुष्य निःसन्देह पृथ्वी के बहुत-से भागों में पाया जाता है जिनको नदियों ने, पहाड़ों ने, वनों और सागरों ने या कृतिम सीमाओं ने विभक्त कर रखा है और मुनष्य की बहुत-सी भिन्न-भिन्न नस्लें और जातियाँ भी अवश्य पाई जाती हैं, जिनके बीच ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और दूसरे कारणों से मनुष्यता के विकास और उन्नति ने विभिन्न रूप ग्रहण किए हैं, किन्तु इस विभिन्नता को दलील ठहरा कर जो व्यक्ति यह कहता है कि हर जाति, हर राष्ट्र और हर भौगोलिक क्षेत्र के लिए ‘धर्म' अर्थात् जीवन-व्यवस्था अलग होनी चाहिए वह सरासर एक व्यर्थ बात करता है। उसकी सीमित दृष्टि बाह्य दृश्यों और बाह्य अवस्थाओं की विभिन्नताओं में उलझ कर रह गई, इस बाहरी विविधता के अन्दर सूक्ष्म मानवीय गुण-धर्म की एकता को वह नहीं पा सका। यदि वास्तव में ये विभिन्नताएँ इतनी महत्व रखती हैं कि उन के आधार पर धर्म अलग-अलग होने चाहिएँ तो मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक जो विभिन्नताएँ एक देश और दूसरे देश, एक वंश और दूसरे वंश के बीच आप पाते हैं उन सब को जितना बढ़ा-चढ़ा कर चाहें लिख लें और फिर उन विभिन्नताओं का शुद्ध वैज्ञानिक विवेचन करें जो स्त्री और पुरुष में पाई जाती हैं, जो हर मनुष्य और दूसरे मनुष्य में पाई जाती हैं, जो एक ही माता और पिता के दो बच्चों में पाई जाती हैं तो कदाचित अत्युक्ति न होगी यदि मैं यह दावा करूं कि ज्ञानात्मक तर्क और विश्लेषण में प्रथम की विभिन्नताओं से ये दूसरी प्रकार की विभिन्नताएँ हर अवस्था में प्रबल ही निकलेंगी, फिर क्यों न कह दीजिए कि हर व्यक्ति की जीवन-व्यवस्था अलग होनी चाहिए ? किन्तु जब आप व्यक्तिगत, जातीय और पारिवारिक बाहुल्य के बीच एकता का एक तत्व और स्थायी तत्व ऐसा पाते हैं जिसके आधार पर एक राष्ट्र या एक देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए एक जीवन-व्यवस्था होना सम्भव समझा जाता है, तो आख़िर किस वस्तु ने आप को रोक दिया है कि राष्ट्रीय, जातीय, मातृभूमि की विविधता के बीच एक और बड़ी आधारात्मक एकता का तत्व आप नहीं पा सकते, जिस पर मानवता की धारणा स्थित हो और जिस के आधार पर समस्त मानव-संसार का एक धर्म या जीवन -व्यवस्था होना सम्भव समझा जाए ? क्या यह वस्तविकता नहीं है कि समस्त भौगोलिक, वांशिक और राष्ट्रीय विभिन्नताओं के होते हुए भी वे प्राकृतिक नियम समान हैं, जिनके अन्तर्गत मुनष्य संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है। वह शारीरिक व्यवस्था समान है जिसके अनुसार मनुष्य की रचना की गई है, वे गुण समान हैं, जिनके आधार पर मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग एक स्थायी जाति ठहरता है, वे प्राकृतिक मांगें और आवश्यकताएँ समान हैं जो मनुष्य के अन्तःकरण में निहित की गई हैं, वह शक्तियाँ समान हैं जिनके समूह को हम मानव वृत्ति कहते हैं और आधार भूत रूप से वे समस्त प्राकृतिक, मानसिक ऐतिहासिक, संस्कृतिक, जीविका सम्बन्धी कारक भी समान हैं जो मानव जीवन में कार्यशील हैं ? यदि यह सत्य है- और कौन कह सकता है कि यह सत्य नहीं है-तो जो सिद्धान्त मनुष्य के कल्याण के लिए ठीक हों उनको विश्वव्यापी होना चाहिए, उनके जातिपरक या वंशपरक या देशपरक होने का कोई कारण नहीं। राष्ट्र और जातियाँ इन सिद्धान्तों के अन्तर्गत अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन और आंशिक रूप से अपने जीवन सम्बन्धी व्यवहारों का प्रबन्ध विभिन्न रीतियों से कर सकती हैं और उनको ऐसा करना चाहिए। किन्तु मनुष्य को मनुष्य होने की दृष्टि से जिस वास्तविक धर्म या जीवन-व्यवस्था की आवश्यकता है वह हर स्थिति में एक ही होनी चाहिए। बुद्धि यह स्वीकार करने से इनकार करती है कि जो वस्तु एक राष्ट्र के लिए सत्य हो वह दूसरे राष्ट्र के लिए असत्य हो जाए और जो एक राष्ट्र के लिए असत्य हो वह दूसरे के लिए सत्य हो जाए।
जीवन का सामयिक विभाजन
इन निरर्थकताओं और आधुनिक काल की ज्ञानात्मक निरर्थकताओं में से एक और बात जो वास्तविकता की दृष्टि से अत्यधिक निरर्थक है, किन्तु आश्चर्य है कि विश्वास की पूरी शक्ति के साथ प्रस्तुत की जाती है, मानव-जीवन का सामयिक विभाजन है अर्थात कहा जाता है कि जो जीवन-व्यवस्था एक युग में सत्य होती है वह दूसरे युग में असत्य हो जाती है। क्योंकि जीवन की समस्याएँ और प्रसंग हर काल में बदल जाते हैं और जीवन-व्यवस्था का सत्य या असत्य होना सरासर उन समस्याओं और प्रसंगों ही की स्थिति पर निर्भर है। यह बात उसी मानव-जीवन के सम्बन्ध में कही जाती है जिसके बारे में साथ ही साथ विकास की बात भी की जाती है। जिसके इतिहास में क्रियाशील नियम भी ढूंढ़े जाते हैं, जिसके पिछले अनुभवों से वर्तमान के लिए शिक्षा और भविष्य के लिए आदेश भी निर्गत किए जाते हैं और जिसके लिए ‘‘मानव प्रकृति'' नाम की एक वस्तु भी प्रमाणित की जाती है। मैं पूछता हूँ क्या आपके पास कोई ऐसा मापक-यन्त्र है जिससे आप मान-जाति की इस निरन्तर ऐतिहासिक गति के बीच काल या युग या समय की वास्तविक सीमाबन्दियाँ कर सकते हों ? और क्या यह सम्भव है कि इन सीमाबन्दियों में से किसी एक रेखा पर उंगली रखकर आप कह सकते हों कि इस रेखा के उस पार जो जीवन-समस्याएँ थीं वे इस पार आकर बिलकुल बदल गईं; और जो परिस्थियाँ उस पार थीं, वे इस पार बाक़ी नहीं ? यदि वास्तव में मानव-इतिहास ऐसे ही अलग-अलग सामयिक भागों में विभाजित है तब तो यूं समझना चाहिए कि एक भाग जो समाप्त हो चुका है वह बाद वाले भागों के लिए केवल एक निरर्थक और व्यर्थ वस्तु हो गई। उसके समाप्त होते ही वह सब कुछ नष्ट हो गया जो मनुष्य ने काल के उस भाग में किया था। उस काल में मनुष्य को जो अनुभव प्राप्त हुए वह बाद वाले काल के लिए अपने अन्दर कोई शिक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे परिस्थितियाँ और वे समस्याएँ ही लुप्त हो गईं जिनमें मनुष्य ने कुछ प्रणालियों या कुछ नियमों का कुछ मूल्यों के लिए प्रयास और चेष्टा का प्रयोग किया था। फिर यह विकास की वार्ता क्यों ? यह जीवन-नियम का अन्वेषण किस लिए ? यह ऐतिहासिक निष्कर्ष किस आधार पर ? जब आप विकास का नाम लेते हैं तो अनिवार्यतः यह इस बात का प्रमाण है कि वहाँ अवश्य कोई वस्तु है जो समस्त परिवर्तनों का विषय बनती है और उन परिवर्तनों के भीतर अपने आपको स्थिर रखते हुए निरन्तर गतिशील है। जब आप जीवन-विधि पर विवाद करते हैं तो यह बात वांछनीय है कि इन अस्थिर परिस्थितियों में इन चलते-फिरते दृश्यों में, इन बनने और बिगड़ने वाली सूरतों में कोई स्थायी और जीवित तथ्य भी है जो अपनी एक विशेष प्रकृति और अपने कुछ स्थायी नियम भी रखती है। जब आप इतिहास से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि इतिहास के इस सुदीर्घ मार्ग पर जो यात्री विभिन्न स्थानों से गुज़रता हुआ आ रहा है, और मंज़िलों पर मंज़िले तय करता हुआ चला आ रहा है, वह स्वयं अपना कोई व्यक्त्त्वि और अपना कोई स्थायी स्वभाव रखता है, जिसके सम्बन्ध में यह आज्ञा लागू की जा सकती है कि वह विशेष परिस्थिति में विशेष रूप से कार्य करता है। वह एक समय में कुछ वस्तुओं को स्वीकार करता है और दूसरे समय में उन्हें अस्वीकार कर देता है और कुछ दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। यह जीवित सत्य, यह स्थायी विषय-परिवर्तन, यह इतिहास के राज-पथ का स्थायी पथिक ही तो है जिसे आप सम्भवतः ‘‘मानवता'' कहते हैं। किन्तु क्या बात है कि जब आप रास्ते की मंज़िलों और उनमें पेश आने वाली परिस्थितियों और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर वार्तालाप आरम्भ करते हैं तो इस वार्तालाप में ऐसे खो जाते हैं कि स्वयं यात्री आपको याद नहीं रहता ? क्या यह सच है कि मंज़िलें और उनकी परिस्थितियाँ और उनकी समस्याएँ बदल जाने से यात्री और उसी वास्तविकता भी बदल जाती है ? हम तो यह देखते हैं कि आदि सृष्टि से आज तक उसकी बनावट बिल्कुल नहीं बदली, उसके विधितत्व वही हैं जो अब से हज़ारों वर्ष पहले थे, उसका स्वभाव वही है, उसकी प्रकृति की मांगे वही है, उसके गुण और उसकी विशेषताएँ वही हैं, उसकी रूचियाँ और उसकी इच्छाएँ वही हैं उसकी शक्तियाँ और उसकी योग्यताएँ वही हैं, उसकी दुर्बलताएँ और अयोग्यताएँ वही हैं, उसके कार्य करने और कार्य-प्रभाव स्वीकार करने और प्रभावित होने के नियम वही हैं, उस पर शासन करने वाली शक्तियाँ वही हैं, और उसका चतुर्दिक विश्व-वातावरण भी वही है। उनमें से किसी वस्तु में भी आदि सृष्टि से आज तक कण मात्र भी अन्तर नहीं आया है। कोई व्यक्ति यह दावा करने का साहस नहीं कर सकता कि इतिहास के बीच में परिस्थितियाँ और उनसे उत्पन्न होने वाली जीवन समस्याओं के परिवर्तन से स्वयं मानवता भी परिवर्तित होती आई है। या वे बुनियादी वस्तुएँ भी परिवर्तित होती रही हैं जो मानवता से सम्बन्ध रखती हैं। फिर जब वास्तविकता यह है तो इस दावे में क्या वज़न हो सकता है कि मनुष्य के लिए जो वस्तु कल अमृत थी वह आज विष है, जो वस्तु कल सत्य थी वह आज असत्य है, जो वस्तु कल मूल्य रखती थी वह आज मूल्यहीन है।
मनुष्य को कैसी जीवन-व्यवस्था की आवश्यकता है ?
सच तो यह है कि व्यक्तियों और समूहों ने इतिहास के बीच में मानवीय गुण-धर्म को और उससे सम्बन्ध रखने वाली बुनियादी वस्तुओं के समझने में धोखा खाकर और कुछ वास्तविकताओं के स्वीकार करने में सीमा से बढ़ कर और कुछ के समझने में भूल करके जो दोषपूर्ण जीवन-विधान समय-समय पर ग्रहण किए और जिन्हें व्यापक मानवता ने अनुभव के बाद दोषपूर्ण पाकर दूसरी ऐसी ही व्यवस्थाओं के लिए स्थान ख़ाली करने पर विवश कर दिया, उनके इतिहास के समीक्षण से यह परिणाम निकाल लिया गया है कि मानवता के लिए अनिवार्यतः हर काल में एक जीवन-व्यवस्था आवश्यक है, जो केवल उसी काल की परिस्थितियों ओर समस्याओं से उत्पन्न हो और उन्हीं का समाधान करने की चेष्टा करे। हालाँकि अधिक सत्यता के साथ इस इतिहास से यदि कोई परिणाम निकाला जा सकता है तो वह यह है कि इस प्रकार की कालसीमित एवं युगीन जीवन-व्यवस्थाएँ या दूसरे शब्दों में पृथ्वी के मौसमी कीड़े-मकौड़ों को बार-बार आज़माने और हर एक की असफलता के बाद उसके दूसरे उत्तराधिकारियों का प्रयोग करने में व्यापक मानवता का समय नष्ट होता है, उसकी राह मारी जाती है । उसका विकास और उन्नति और अपने सम्पूर्ण ध्येय की ओर उसकी यात्रा में अत्यन्त कठिनाई पेश आती है। वास्तव में उसको आवश्यकता है और अति आवश्यकता है ऐसी जीवन-व्यवस्था की जो स्वयं उसकी और उससे सम्बन्ध रखने वाली समस्त वास्तविकताओं को जानकर, विश्वव्यापी, स्थायी और सुदृढ़ नियमों पर स्थापित की जाए, जिसे लेकर वह वर्तमान और भविष्य की समस्त परिवर्तित परिस्थितियों से भली-भांति पार हो सके, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल कर सके, जीवन के मार्ग पर गिरते-पड़ते नहीं, बल्कि दौड़ते और भागते अपने लक्ष्य-स्थान की ओर बढ़ सके।
क्या मनुष्य ऐसी व्यवस्था स्वयं बना सकता है ?
यह है उस ‘दीन' (धर्म विशेष या जीवन-प्रणाली या जीवन-व्यवस्था) का स्वरूप, जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है। अब हमें देखना चाहिए कि यदि मनुष्य ईश्वर की सहायता से बेपरवाह होकर स्वयं अपने लिए इस प्रकार का एक धर्म बनाना चाहे तो क्या वह इस प्रयास में सफल हो सकता है ? यह प्रश्न मैं आपके सामने पेश न करूंगा कि क्या मनुष्य अब तक ऐसा स्वयं बनाने में सफल हुआ है ? क्योंकि इसका उत्तर तो सर्वथा नहीं में है। स्वयं वे लोग भी जो आज बड़े-बड़े ऊॅंचे दावों के साथ अपने-अपने धर्म पेश कर रहे हैं और उनके लिए एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, यह दावा नहीं कर सकते कि उनमें से किसी का पेश किया हुआ धर्म उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनके लिए मनुष्य को मनुष्य की हैसियत से एक ‘‘अद-दीन'' (मुख्य-धर्म) की आवश्यकता है। किसी का धर्म जातीय है, किसी का भौगोलिक, किसी का वर्गीय और किसी का दीन उत्पन्न ही उस काल के तक़ाज़ों से हुआ है जो अभी कल ही गुज़रा है। वह युग जो कल आने वाला है उसकी परिस्थितियों और समस्याओं के सम्बन्ध में पेशगी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनमें भी वह काम दे सकेगा या नहीं ? क्योंकि जो काल अब बीत रहा है अभी तो उसी की ऐतिहासिक आवश्यकताओं का समीक्षण बाक़ी है। इसी लिए मैं यह प्रश्न नहीं कर रहा हूँ कि मनुष्य ऐसा धर्म बनाने में सफल हुआ है या नहीं, बल्कि यह कह रहा हूँ कि सफल हो भी सकता है या नहीं ?
यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में सरसरी तौर पर विवाद उचित नहीं, यह मानव-जीवन के निर्णायक प्रश्नों में से एक है। इसलिए पले भली-भांति समझ लीजिए कि वह वस्तु क्या है जिसके निर्माण करने का प्रश्न सामने है और उस व्यक्ति की योग्याताएँ क्या हैं जिसके सम्बन्ध में यह पूछा जा रहा है कि वह इसका निर्माण कर सकता है या नहीं?
धर्म-विशेष की विशेषता
मनुष्य के लिए जिस धर्म-विशेष (अद्-दीन) की आवश्यकता मैंने अभी सिद्ध की है उसका तात्पर्य कोई ऐसा विस्तृत विधान नहीं है जिसमें हर काल और हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए समस्त छोटे-बड़े भाग तक निश्चित एवं संपादित हों और जिसकी उपस्थिति में मनुष्य का काम केवल उसके अनुसार कार्य करना हो, बल्कि वास्तव में उसका अभिप्राय ऐसे व्यापक सिद्धान्तों से है जो सृष्टि के आदि से अन्त तक, समस्त परिस्थितियों में मनुष्य का पथ-प्रदर्शन कर सकें। उसके विचार, दृष्टिकोण प्रयत्न तथा प्रयास और आगे बढ़ने के लिए ठीक दिशा निश्चित कर सकें और उसे अशुद्ध प्रयोगों में समय, परिश्रम और शक्ति नष्ट करने से बचा सकें। इस उद्देश्य के लिए मनुष्य की सब से प्रथम आवश्यकता यह है कि उसे इस बात का अनुमान और अटकल नहीं, बल्कि ज्ञान हो कि उसकी और सृष्टि की यथार्थता क्या है ? और सृष्टि में उसकी स्थिति क्या है ? फिर उसे इस बात के समझ बैठने की नहीं बल्कि जानने की आवश्यकता है कि क्या जीवन बस यही सांसारिक जीवन है या यह सम्पूर्ण जीवन का एक आरम्भिक भाग है ? क्या यात्रा बस जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की है या यह पूरी यात्रा में से केवल एक क्रम है ? फिर उसके लिए अनिवार्य है कि एक ऐसा जीवन-ध्येय उसके लिए निश्चित हो जो वास्तविकता की दृष्टि से, न कि केवल इच्छा के आधार पर, वास्तव में मानव जीवन का ध्येय हो, जिसके लिए वास्तव में मनुष्य पैदा किया गया हो और जिसके साथ हर व्यक्ति, व्यक्तियों का हर समूह और पूर्ण रूप से समस्त मानवता के ध्येय, समस्त कालों में बिना किसी संघर्ष और टकराव के एकरूप हो सकें। फिर उसको नैतिकता के ऐसे सुदृढ़ और सर्वव्यापी सिद्धान्तों की आवश्यकता है जो उसकी प्रकृति की समस्त विशेषताओं के साथ एकरूपता भी रखते हों और समस्त सम्भव परिस्थितियों पर सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से ठीक उतर सकते हों; ताकि वह उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण कर सके। इन्हीं के पथ-प्रदर्शन में जीवन-यात्रा की हर मंज़िल और उसकी परिस्थिति में मौजूद समस्याओं का समाधान कर सके और इस ख़तरे में न पड़े कि परिवर्तनशील और समस्याओं के साथ-साथ नैतिकता के सिद्धान्त बनाता और बदलता चला जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में एक सिद्धान्तरहित निरा अवसरवादी (Characterless Opportunist) बन कर रह जाए। फिर उसको संस्कृति के ऐसे विस्तृत और पूर्ण सिद्धांतों की आवश्यकता है जो मानव-समाज की वास्तविकता और ध्येय और उसकी प्राकृतिक मांगों को समझ कर बनाए जाएँ जिनमें न्यूनता, अधिकता और असमता न हो, जिनमें सभी मनुष्यों के सामूहिक लाभ पर दृष्टि रखी गई हो और जिसका अनुसरण करके हर काल में मानव-जीवन के हर पहलू के निर्माण, रचना और उन्नति का प्रयत्न किया जा सके। फिर उसे व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक नीति और व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्न और कर्म को ठीक यात्रा-दिशा का यात्री और पथ-भ्रष्टता से सुरक्षित रखने के लिए ऐसी पूर्ण सीमाओं की आवश्यकता है जो जीवन के राजमार्ग पर पथ-चिन्ह का काम दें, और हर मोड़, हर चैराहे और आशंकापूर्ण स्थान पर उसे सचेत कर दें कि तेरा रास्ता उधर नहीं बल्कि इधर है। फिर उसको कुछ ऐसे संकोचरहित सक्रिय व्यावहारिक नियमों की आवश्यकता है जो अपने तथ्य की दृष्टि से स्थायी और सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए अनुसरणीय हों और मानव-जीवन को उस वास्तविक उद्देश्य, उस जीवन-परिणाम, उस जीवन-ध्येय, उन नैतिक और सांस्कृतिक सिद्धान्तों और उन कार्य-सीमाओं से सदैव सम्बन्धित रखें जिनका निश्चय उस ‘‘अद्-दीन'' में किया गया हो।
यह है वह वस्तु जिसकी रचना का प्रश्न सामने है। अब विचार कीजिए क्या मनुष्य ऐसे साधन रखता है जिनसे वह स्वयं अपने लिए एक ऐसा ‘‘अद्-दीन'' निर्माण कर सके ?
मानवीय साधन की समीक्षा
मनुष्य के पास अपना ‘‘दीन'' (धर्म) या जीवन-प्रणाली प्राप्त करने के साधन चार से अधिक नहीं हैं। पहला साधन इच्छा है, दूसरा साधन बुद्धि है, तीसरा साधन निरीक्षण और अनुभव है चैथा साधन पिछले अनुभवों के ऐतिहासिक रिकार्ड हैं। सम्भवतः इनके अतिरिक्त किसी पाँचवे साधन का पता नहीं बताया जा सकता । इन चारों साधनों का जितना पूर्ण विवेचन करके आप देख सकते हों देखिए कि क्या ये ‘अद-दीन' (मुख्य धर्म) के निर्माण करने में मनुष्य की सहायता कर सकते हैं ? मैंने अपनी आयु का एक मुख्य भाग इस प्रश्न के अन्वेषण में व्यय किया है और अन्ततः इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ये साधन ‘‘मुख्य धर्म'' के निमार्ण में तो सहायता नहीं कर सकते, हाँ, मानव-प्रणाली के अतिरिक्त यदि कोई दिव्य पथ-प्रदर्शक ‘मुख्य धर्म' को प्रस्तुत कर दे तो उसे समझने, परखने, पहचानने और उसके अनुसार जीवन की विस्तृत व्यवस्था का समय-समय पर निर्माण करते रहने में अवश्य सहायक बन सकते हैं।
इच्छा
पहले इच्छा को लीजिए, क्या यह मनुष्य की पथ-प्रदर्शक बन सकती है ? यद्यपि यह मनुष्य के भीतर कर्म की वास्तविक प्रेरक है, किन्तु इसकी मुख्य प्रकृति में जो दुर्बलताएँ मौजूद हैं उनके कारण यह पथ-प्रदर्शन के योग्य कभी नहीं हो सकती। अकेले पथ-प्रदर्शन करना तो दूर रहा, बुद्धि और ज्ञान को भी प्रायः इस ने पथ-भ्रष्ट किया है। इसको शिक्षा-दीक्षा से चाहे कितना ही परिष्कृत बना दिया जाए, हर अवस्था में अन्तिम निर्णय जब कभी इस पर छोड़ा जाएगा वह अवश्य 99 प्रतिशत परिस्थितियों में अनुचित मार्ग का ही निर्णय करेगी, क्योंकि इसके भीतर जो मांगें पाई जाती हैं वे उसको शुद्ध निर्णय करने के स्थान पर ऐसा निर्णय करने पर विवश करती हैं जिनसे मनचाही वस्तु किसी न किसी प्रकार शीध्र और सरलता से प्राप्त हो जाए। यह मनोदशा ‘‘मानवीय इच्छा'' की स्वाभाविक दुर्बलता है। अतः चाहे एक व्यक्ति की इच्छा हो या एक वर्ग की हो या वह सार्वजनिक इच्छा (General Will) हो जिसकी रूसो (Russecau) ने चर्चा की है। सारांश यह कि किसी प्रकार की मानव इच्छा में भी प्राकृतिक रूप से यह योग्यता नहीं है कि एक ‘मुख्य धर्म' के निर्माण करने में सहायक बन सके। बल्कि जहाँ तक मुख्य समस्याओं-उदाहरणः मानव-जीवन की वास्तविकता, उसके परिणाम और उसके उद्देश्य का सम्बन्ध है, उनको हल करने में तो यह किसी प्रकार सहायक बन नहीं सकती।
बुद्धि
फिर बुद्धि को लीजिए। उसकी समस्त उत्तम योग्यताएँ सिद्ध, मानव जीवन में उसकी प्रधानता भी अकाट्य और यह भी स्वीकार कि मनुष्य के भीतर यह बहुत बड़ी पथ-प्रदर्शक शक्ति है। लेकिन इस प्रश्न को जाने दीजिए कि मनुष्य के लिए ‘‘मुख्य धर्म'' किसकी बुद्धि निर्माण करेगी ? आपकी ? हमारी ? समस्त मानवों की ? या किसी विशिष्ट गिरोह के लोगों की ? या किसी पिछले युग वालों की ? या आगे आने वालों की ? प्रश्न केवल यह है कि ‘‘मानव बुद्धि'' की सीमाओं का विवेचन करने के बाद क्या कह सकते हैं कि ‘मुख्य-धर्म' के निर्माण करने में उस पर भरोसा किया जा सकता है ? उसके सारे फ़ैसले अवलम्बित हैं उस सामग्री पर जो इन्द्रियाँ, उसको संग्रह करके दें। वे अशुद्ध सामग्री एकत्रित करके देंगी तो यह अशुद्ध निर्णय कर देगी, वह अपूर्ण-सामग्री एकत्रित करके देंगी तो यह अपूर्ण फ़ैसला कर देगी।
और जिन विषयों में वह कोई सामग्री प्रस्तुत न करेंगी उनके प्रति यदि वह आत्म-परिचित है तो कोई फ़ैसला न करेगी और यदि वह स्वतः आत्मज्ञान भ्रष्ट है तो अन्धकार में चैमुखी तीर चलाती रहेगी। यह सीमितताएँ जिस बुद्धि बेचारी के साथ लगी हुई हैं वह आख़िर कैसे इस योग्य हो सकती है कि समस्त मनुष्यों के लिए ‘धर्म-विशेष' के निर्माण का कष्ट उसे दिया जाए ? ‘धर्म-विशेष' बनाने का काम जिन महान समस्याओं के समाधान पर आश्रित है उनमें इन्द्रियाँ सिरे से कोई सामग्री प्रस्तुत ही नहीं करतीं। फिर क्या उन समस्याओं का निर्णय कल्पनाओं, निरर्थक अनुमानो और कोरी भ्रांतियों से किया जाएगा ? ‘धर्म-विशेष' बनाने के लिए जिन स्थायी नैतिक मूल्यों का निर्धारण अनिवार्य है उनके लिए इन्द्रियाँ बहुत ही अपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती हैं। फिर क्या बुद्धि से यह आशा की जा सकती है कि वह अपूर्ण सामग्री पर शुद्ध और पूर्ण मूल्य निर्धारित करेगी? इसी प्रकार ‘धर्म-विशेष' के जो दूसरे घटक तत्व मैंने बयान किए हैं उनमें से किसी एक तत्व के लिए भी इन्द्रियों से सर्वथा शुद्ध और पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके आधार पर बुद्धि एक सम्पूर्ण और व्यापक व्यवस्था बना सके। और इस पर यह भी कि बुद्धि के साथ इच्छा का अंश स्थायी रूप से सम्मिलित रहता है जो उसे ठेठ बौद्धिक निर्णय देने से रोकता है। और उसकी सत्यवादिता को कुछ-न-कुछ टेढ़ की ओर आकर्षित करके ही छोड़ता है। अतः यदि यह मान भी लिया जाए कि मानव-बुद्धि इन्द्रियों की एकत्रित की हुई सामग्री के सम्पादन और उससे तर्क प्राप्त करने में कोई भूल न करेगी तब भी अपनी दुर्बलताओं के कारण वह इतना बलबूता नहीं रखती कि इतने बड़े काम का बोझ उस पर डाला जा सके। यह बोझ डालना उस पर भी अन्याय है और स्वयं अपने ऊपर भी।
ज्ञान-विज्ञान
अब तीसरे साधन को लीजिए अर्थात् वह ज्ञान जो प्रयोग और निरीक्षिण से प्राप्त होता है। मैं इस ज्ञान के मूल्य को स्वीकार करने में किसी विद्यार्थी से पीछे नहीं हूँ और न लेशमात्र उसका अनादर करना पसन्द करता हूँ। किन्तु उसकी सीमितताओं की उपेक्षा करके उसे वह विस्तृत रूप देना, जो वास्तव में उसे प्राप्त नहीं है, मेरे निकट अज्ञानता है। ‘मानव-ज्ञान' की यथार्थता पर जिस व्यक्ति की भी दृष्टि होगी वह इस बात को मानने से इनकार न करेगा कि जहाँ तक महान् समस्याओं का सम्बन्ध है, उनकी तह तक उसकी पहुँच असम्भव है। क्योंकि मनुष्य को वह साधन प्राप्त ही नहीं हैं जिनसे वह उस तक पहुँच सके। न वह उसको सीधे-सीधे देख सकता है और न प्रयोग और निरीक्षण के अन्तर्गत आनेवाली वस्तुओं से तर्क प्राप्त करके उसके सम्बन्ध में ऐसा मत स्थिर कर सकता है जो ‘ज्ञान' का आधार बन सकता हो। अतः ‘धर्म-विशेष' निर्माण करने के लिए जिन समस्याओं का हल मालूम करना सबसे पहली वांछनीय आवश्यकता है वह तो ज्ञान की पहुँच से बाहर ही है। अब रहा यह प्रश्न कि नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक नियम और पथ भ्रष्टता से बचाने वाली सीमा निर्धारित करने का कार्य क्या ज्ञान के हवाले किया जा सकता है या नहीं ? तो इस विवाद को छोड़ते हुए कि यह कार्य किस व्यक्ति या किस समूह का या किस काल का ज्ञान सम्पन्न करेगा, हमें यह देखना चाहिए कि ज्ञानात्मक रीति से कार्य सम्पादित करने के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं ? इसके लिए पहली शर्त यह है कि उन समस्त प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त हो जिनके अन्तर्गत मनुष्य इस संसार में जी रहा है। इसके लिए दूसरी शर्त यह है कि स्वयं मनुष्य के अपने जीवन से जो ज्ञान सम्बन्ध रखते हैं वह पूर्ण हों, इसके लिए तीसरी शर्त यह है कि इन दोनों प्रकार के ज्ञान अर्थात् सृष्टि-ज्ञान और मानव-ज्ञान की जानकारियाँ एकत्रित हों और कोई पूर्ण-बुद्धि उनको शुद्ध रूप से सम्पादित कर उनसे शुद्ध तर्क प्राप्त करके मनुष्य के लिए नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक नियमों और पथभ्रष्टता से बचाने वाली सीमाओं को निर्धारित करे। ये शर्तें न इस समय तक पूरी हुई हैं न आशा की जा सकती है कि पाँच हज़ार वर्ष बाद पूरी हो जाएँगी।सम्भव है कि मानवता की मृत्यु से एक दिन पहले ये पूरी हो जाएँ, किन्तु उस समय उनका लाभ ही क्या होगा ?
इतिहास
अन्त में उस ज्ञान-साधन को लीजिए जिसे हम पिछले मानव-अनुभवों का ऐतिहासिक रिकार्ड या मानवता का कर्म-पत्र कहते हैं। उसके महत्व और उसके लाभों से मुझे इनकार नहीं । किन्तु मैं कहता हूँ और विचार करेंगे तो आप भी मान लेंगे कि ‘धर्म-विशेष' का निर्माण करने का महान् कार्य पूरा करने के लिए यह भी अपूर्ण है। मैं यह प्रश्न नहीं करता कि यह रिकार्ड अतीत से वर्तमान के लोगों तक शुद्धता और पूर्णता के साथ पहुँचा भी या नहीं ? मैं यह भी नहीं पूछता कि इस रिकार्ड की सहायता से ‘धर्म-विशेष' निर्माण करने के लिए मानवता का प्रतिनिधि किस मष्तिष्क को बनाया जाएगा। हीगल के मस्तिष्क को ? मार्क्स के मष्तिष्क को ? अर्नेस्ट हीगल के मष्तिष्क को ? या किसी और मस्तिष्क को ? मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि भूत, वर्तमान, या भविष्य में किस तिथि तक का रिकार्ड एक ‘धर्म-विशेष' निर्माण करने के लिए पूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर सकेगा ? उस तिथि के पश्चात् उत्पन्न होने वाले भाग्यवान हैं, बाक़ी बचे उससे पहले गुज़र जाने वाले तो उनका बस ईश्वर ही रक्षक है।
नैराश्यपूर्ण परिणाम
यह संक्षिप्त संकेत जो मैंने किए हैं मुझे आशा है कि मैंने उनमें कोई वैज्ञानिक या तार्किक भूल नहीं की है। और यदि मनुष्य के साधनों का यह समीकरण जो मैंने किया है ठीक है तो फिर हमें कोई वस्तु इस विश्वास तक पहुँचने से रोक नहीं सकती कि मनुष्य अपने लिए कोई कच्चा, पक्का, ग़लत-सलत, सामयिक और स्थानीय ‘‘धर्म'' तो निर्माण कर सकता है, किन्तु वह चाहे कि ‘‘धर्म विशेष'' (अद्-दीन) का निर्माण कर सके तो यह नितांत असम्भव है। पहले भी असम्भव था, आज भी असम्भव है और भविष्य के लिए भी इसकी सम्भावना से पूर्ण निराशा है।
अब यदि पथ-प्रदर्शन के लिए किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, जैसा नास्तिकों का मत है तो मनुष्य के लिए उचित है कि आत्महत्या कर ले। जिस यात्री के लिए न कोई पथ-प्रदर्शक हो और न जिसके पास अपना मार्ग मालूम करने के साधन हों, उसके लिए निराशा और पूर्ण निराशा के अतिरिक्त कुछ भाग्य में नहीं। उससे कोई सहानुभूति रखने वाला इसके सिवा उसे और क्या परामर्श दे सकता है कि मार्ग में पड़े हुए किसी पत्थर से सिर टकरा कर अपनी मुश्किल आसान कर ले। और यदि ईश्वर है, किन्तु पथ-प्रदर्शन वाला ईश्वर नहीं है, जैसा कि कतिपय दार्शनिक और वैज्ञानिक ढंग के ईश्वरवादियों का विचार है तो यह और भी अधिक चिन्ताजनक परिस्थिति है। जिस ईश्वर ने समस्त सृष्टि के अस्तित्व, विकास और उन्नति के लिए हर उस वस्तु के उपलब्ध करने का प्रबन्ध किया है जिसकी आवश्यकता की कल्पना की जा सकती हो, किन्तु एक नहीं किया तो केवल मनुष्य की उस सबसे बड़ी आवश्यकता का प्रबन्ध जिसके बिना पूरी मानवजाति का जीवन अशुद्ध हुआ जाता है, उसके बनाए हुए संसार में रहना एक विपत्ति है, ऐसी कठिन विपत्ति जिससे बढ़कर किसी दूसरी विपत्ति की कल्पना सम्भव नहीं। आप निर्धनों, दरिद्रों, घायलों, अत्याचार-पीड़ितों और दुखी लोगों की विपत्ति पर क्या रोते हैं ? रोइए उस पूरी मानव-जाति की विपत्ति पर जो इस असहाय स्थिति में छोड़ दी गई है कि बार-बार ग़लत अनुभव करके असफल होती है, ठोंकरे खाकर गिरती है और फिर उठकर चलती है, ताकि फिर ठोकर खाए। हर ठोकर पर देश के देश और राष्ट्र के राष्ट नष्ट हो जाते हैं। उस बेचारी को अपने जीवन-ध्येय तक का पता नहीं है, कुछ नहीं जानती कि किस उद्देश्य के लिए प्रयास और कर्म करे और किस ढंग पर करे। यह सब कुछ वह ईश्वर देख रहा है जिसने उसे धरती पर जन्म दिया है। किन्तु बस वह उसे उत्पन्न करने से सम्बन्ध रखता है, पथ-प्रदर्शन की परवाह नहीं करता।
आशा की एक ही किरण
इस चित्र के बिल्कुल विपरीत क़ुरआन हमारे सामने परिस्थिति का एक दूसरा चित्र उपस्थित करता है। वह कहता है कि ईश्वर केवल उत्पन्न कर देने वाला नहीं है बल्कि पथ-प्रदर्शन करने वाला भी है। उसने सृष्टि में से हर वस्तु को वह ज्ञानपथ प्रदान किया जो उसकी प्रकृति के अनुसार उसके लिए आवश्यक है।
‘‘अल्लज़ी आता कुल-ल शैइन् ख़-ल-क़हू सुम-म हदा'
अर्थात्-‘ईश्वर' वही है जिसने हर वस्तु को उसका अस्तित्व प्रदान किया और फिर उसे मार्ग दिखाया। (क़ुरआन)
यदि इसका प्रमाण चाहो तो जिस चींटी, जिस मक्खी, जिस मकड़ी को चाहो पकड़ कर देख लो। वही ईश्वर मनुष्य का भी पथ-प्रदर्शन करने वाला है। अतः मनुष्य के लिए शुद्ध कार्य-प्रणाली यह है कि स्वच्छंदता छोड़कर उसके आगे नत-मस्तक हो जाए और जिस सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्था या ‘‘अद्-दीन'' ‘धर्म-विशेष' का आदेश उसने अपने पैग़म्बरों (सन्देष्टाओं) द्वारा भेजा है उसका अनुसरण करना स्वीकार कर ले।
देखिए एक ओर तो वह परिणाम है जो मनुष्य की शक्तियों और उसके साधनों का समीक्षण करने से हमको प्राप्त होता है और दूसरी ओर क़ुरआन का यह दावा है। हमारे लिए इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं कि या तो उस दावे को स्वीकार करें या फिर अपने आपको उस निराशा के हवाले कर दें जिसके अन्धकार में कहीं नाम के लिए भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती। वास्तव में परिस्थिति यह है ही नहीं कि ‘अद-दीन' प्राप्त होने के दो साधन उपस्थित हों और प्रश्न यह हो कि हम उनमें से किस साधन से सहायता लें। वास्तविक परिस्थिति यह है कि ‘अद्-दीन' जिस साधन से हमको मिल सकता है वह केवल एक है और चुनाव का प्रश्न केवल इस बारे में हैं कि क्या हम इस एक मात्र साधन से सहायता लें या इसकी सहायता से लाभ उठाने की जगह अन्धकार में भटकते फिरने को पसन्द करें ?
क़ुरआन के तर्क
यहाँ तक जो तर्क मैंने प्रस्तुत किया है वह तो हमको केवल इस सीमा तक पहुँचाता है कि हमारे कल्याण के लिए क़ुरआन के इस दावे को स्वीकार किए बिना कोई मार्ग नहीं है। अर्थात् दूसरे शब्दों में नास्तिक नहीं हो सकता तो बाध्य होकर आस्तिक हो जा, किन्तु क़ुरआन अपने दावे के समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत करता है वह इससे अत्यधिक महान् और श्रेष्ठ हैं क्योंकि वह हमें अरुचि से मुसलमान (आज्ञापालक) होने के स्थान पर प्रसन्नता और सुरुचि से मुसलमान होने के लिए तत्पर करते हैं। उसके बहुत से तर्कों में से चार तर्क सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और उन्हीं को उसने बार-बार निरन्तर प्रस्तुत किया है।
1-मनुष्य के लिए ‘‘इस्लाम'' (आज्ञापालन) ही एक शुद्ध जीवन-प्रणाली है, इसलिए कि यही वास्तविकता के अनुकूल है और इसके अतिरिक्त हर दूसरा मार्ग सत्यता के विरुद्ध है।
‘‘ क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अतिरिक्त कोई और दीन चाहते हैं, हालांकि वे सब वस्तुएँ जो आकाशों में हैं और जो पृथ्वी में है चाहे-अनचाहे उसी के आगे नतमस्तक हैं और उसी की ओर उन्हें पलट कर जाना है।'' (क़ुरआन-3:83)
2-मनुष्य के लिए यही एक शुद्ध जीवन-प्रणाली है, क्योंकि यही सत्य है और न्याय की दृष्टि से इसके अतिरिक्त कोई दूसरा आचार शुद्ध नहीं हो सकता।
‘‘वास्तव में तुम्हारा पालनकर्ता (प्रभु और आज्ञादाता) तो अल्लाह है जिसने आकाशों और पृथ्वी को छः युगों में उत्पन्न किया और फिर अपने राज-सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, जो दिन को रात्रि का वस्त्र उढ़ाता है और फिर रात्रि का पीछा करते हुए दिन तीव्र गति से दौड़ा आता है। सूर्य, चन्द्रमा, और तारे सबके सब जिसकी आज्ञा के अधीन हैं, सुनो, सृष्टि उसी की है और आज्ञा भी उसी की , बड़ी बरकत वाला है वह सृष्टि का पालनकर्ता।'' (क़ुरआन-7:54)
3-मनुष्य के लिए यही आचरण शुद्ध है क्योंकि समस्त सत्यों का वास्तविक ज्ञान केवल परमेश्वर ही को है और निर्दोष पथ-प्रदर्शन केवल वही कर सकता है।
‘‘वास्तव में अल्लाह से न पृथ्वी की कोई वस्तु छिपी हुई है और न आकाश की।'' (क़ुरआन-3:5)
‘‘जो कुछ लोगों के सामने है उसे भी वह जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है वह भी उसके ज्ञान में है और लोग उसकी जानकारियों में किसी वस्तु को भी घेर नहीं सकते उन वस्तुओं के अतिरिक्त जिनका ज्ञान वह स्वयं उनको देना चाहे।'' (क़ुरआन-2:255)
‘‘ऐ पैग़म्बर ! कह दो कि निःसन्देह वास्तविक पथ-प्रदर्शन केवल अल्लाह ही का पथ-प्रदर्शन है।'' (क़ुरआन-6:71)
4-मनुष्य के लिए यही एक सीधी राह है क्योंकि इसके बिना न्याय सम्भव नहीं। इसके अतिरिक्त जिस मार्ग पर भी मनुष्य चलेगा वह अन्ततः अन्याय ही की ओर जाएगा।
‘‘जो अल्लाह की ठहराई हुई सीमाओं का उल्लंघन करते हैं वही अन्यायी है।'' (क़ुरआन-2:229)
‘‘जो अल्लाह के उतारे हुए आदेश के अनुसार निर्णय नहीं करते वही लोग अन्यायी हैं।'' (क़ुरआन-5:45)
ये तर्क हैं जिनके आधार पर हर औचित्य-प्रिय मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वह ईश्वर के आगे मस्तक नत कर दे और मार्ग-प्राप्ति के लिए उसी के सम्मुख उपस्थित हो!
ईश्वरीय पथ-प्रदर्शन के परखने की कसौटी
अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक समझता हूँ जो अनिवार्यतः इस स्थान पर पहुँच कर हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है और अपने अध्ययन एवं शोध के बीच स्वयं मेरे मन में भी उत्पन्न हो चुका है। वह प्रश्न यह है कि क्या हम उस व्यक्ति की बात मान लें जो एक धर्म हमारे सामने इस दावे के साथ प्रस्तुत कर दे कि यह ईश्वर की ओर से है ? यदि ऐसा नहीं है तो आख़िर हमारे पास वह कौन-सी कसौटी है जिससे हम मनुष्य के बनाए हुए धर्म और ईश्वरीय आदेश के धर्म के अन्तर को समझ सकें? इसका उत्तर यद्यपि बड़ा लम्बा-चैड़ा विवेचनात्मक विवाद चाहता है, किन्तु मैं यहाँ संक्षिप्त संकेतों में वह चार बड़ी कसौटियाँ उपस्थित करूंगा जो मानवीय विचार और ईश्वरीय विचार को एक दूसरे से भिन्न करती हैं।
1-मानवीय विचार की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान की त्रुटि और सीमितता का प्रभाव अनिवार्यतः पाया जाता है और इसके विपरीत ईश्वरीय विचार में असीमित ज्ञान और वास्तविक ज्ञान की, श्रेष्ठता पूर्णरूपेण प्रकट होती है। जो वस्तु ईश्वर की ओर से होगी उसमें आप ऐसी कोई वस्तु नहीं पा सकते जो कभी किसी काल में किसी सिद्ध वैज्ञानिक सत्य के विरुद्ध हो या जिसके विषय में यह सिद्ध किया जा सके कि उसके रचयिता की दृष्टि से सत्य का अमुक पक्ष ओझल रह गया । किन्तु इस खोज की कसौटी का प्रयोग करते हुए यह बात न भूल जाइए कि ज्ञान और ज्ञानात्मक सिद्धान्त में बड़ा अन्तर है। एक समय जो ज्ञानात्मक कल्पना और ज्ञानात्मक सिद्धान्त मस्तिष्कों पर छाए हुए होते हैं अधिकांश भ्रान्ति से उनको ज्ञान समझ लिया जाता है, हालाँकि उनके असत्य होने की भी उतनी ही सम्भावना होती है जितनी उनके सत्य होने की, और ज्ञान के इतिहास में ऐसी बहुत कम कल्पनाओं तथा दृष्टिकोणों का पता बताया जा सकता है जो अन्ततः ‘ज्ञान' सिद्ध हुए हों।
2-मानवीय विचार की दूसरी बड़ी दुर्बलता उसका संकुचित दृष्टिकोण है और इसके विपरीत ईश्वरीय विचार में अति विस्तृत दृष्टिकोण पाया जाता है। जब आप ईश्वरीय विचार से निकलती हुई किसी वस्तु को देखेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा मानो उसका रचयिता आदि से अन्त तक देख रहा है, पूरी सृष्टि को देख रहा है, समस्त वास्तविकताओं को एक दृष्टि में देख रहा है। उसकी तुलना में बड़े-से-बड़े दार्शनिक और विचारक का विचार भी एक बालक का विचार ज्ञात होगा।
3-मानवीय विचार की तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि उसमें तत्वर्शिता, सूझ-बूझ, भावों और इच्छाओं के साथ वे कहीं साठं-गांठ और संधि करते दिखाई दे ही जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वरीय विचार में बेलाग तत्वदर्शिता और शुद्ध बुद्धिमता की महानता इतनी प्रकट होती है कि उसकी आज्ञाओं में कहीं आप भावात्मक झुकाव का चिन्ह नहीं दिखा सकते।
4-मानवीय विचार की एक और बड़ी दुर्बलता यह है कि जो जीवन-व्यवस्था वह स्वयं निर्माण करेगा उसमें पक्षपात, मनुष्य और मनुष्य के बीच बुद्धि-विरुद्ध भेद, और ज्ञानहीन आधारों ही पर किसी को किसी पर श्रेष्ठता देने का तत्व अनिवार्यतः पाया जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य की कुछ व्यक्तिगत रुचियाँ होती हैं जो कुछ मनुष्यों के साथ सम्बन्धित होती हैं और कुछ मनुष्यों के साथ सम्बन्धित नहीं होतीं। इसके विपरीत ईश्वरीय विचार से निकली हुई जीवन-व्यवस्था ऐसी प्रत्येक वस्तु से पूर्णरूपेण शुद्ध होगी। इस कसौटी पर आप हर उस जीवन-व्यवस्था को जांच कर देखिए जो अपने आप को ईश्वर की ओर से ‘‘अद्-दीन'' (धर्म-विशेष) कहती हो। यदि वह मानवीय विचार की उन समस्त विशेषताओं से रिक्त हो और फिर पूर्णता और सर्वव्यापकता की वह श्रेष्ठता भी रखती हो जो इसके पूर्व मैंने ‘‘अद्-दीन'' की आवश्यकता सिद्ध करते हुए बयान की है तो कोई कारण नहीं कि आप उस पर विश्वास करने में हिचक से काम लें।
ईमान की मांगें
अब मुझे अपने विषय के बुनियादी प्रश्नों में से अन्तिम प्रश्न पर कुछ वार्ता करनी है और वह यह है कि मनुष्य जब क़ुरआन के इस दावे को स्वीकार कर ले और उस ‘‘अद्-दीन'' पर ईमान ले आए जिसके ईश्वर की ओर से होने का विश्वास उसे प्राप्त हो गया हो तो उसे स्वीकार करने और ईमान लाने की मांगें क्या हैं ?
मैं आरम्भ में निवेदन कर चुका हूँ कि इस्लाम के अर्थ झुक जाने, हथियार डाल देने, अपने आपको सौंप देने के हैं। इस झुकाव, समर्पण और हथियार डाल देने के साथ स्वच्छन्दता, स्वाधीनता और विचार एवं आचरण की स्वतन्त्रता कभी नहीं निभ सकती। जिस धर्म पर भी आप विश्वास करें आप को अपना पूरा व्यक्तित्व उसके हवाले कर देना होगा। अपनी किसी वस्तु को भी आप उसके अनुसरण से अलग नहीं रख सकते। विश्वास (ईमान) की मांग यह है कि वह आपके हृदय और मस्तिष्क का धर्म हो, आपकी आंख और कान का धर्म हो, आपके हाथ और पांव का धर्म हो, आपके पेट और धड़ का धर्म हो, आपके क़लम और ज़ुबान का धर्म हो, आपके समय और आपके परिश्रमों का धर्म हो, आपके प्रयास और कार्य का धर्म हो, आपके प्रेम और घृणा का धर्म हो, आपकी दोस्ती और दुश्मनी का धर्म हो, अर्थात् आपके व्यक्तित्व का कोई भाग और कोई पक्ष भी इस धर्म से बाहर न हो, जिस वस्तु को भी जितना और जिस रूप से आप उस धर्म-क्षेत्र से बाहर और उसके अनुसरण से अलग रखेंगे, समझ लीजिए कि उतना ही आपके ईमान के दावे में झूठ सम्मिलित है और हर सत्यवादी मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को झूठ से बचाए रखने की अधिक से अधिक चेष्टा करे।
फिर यह भी मैं आरम्भ में निवेदन कर चुका हूँ कि मानव-जीवन एक सर्वस्व है जिसे विभागों में बांटा नहीं जा सकता। अतः मानव के सम्पूर्ण जीवन का एक ही धर्म होना चाहिए। दो-दो और तीन-तीन धर्मों का एक ही समय में अनुसरण इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि यह विश्वास के डांवाडोल और बौद्धिक-निर्णय के विचलित होने का प्रमाण है। जब वास्तव में किसी धर्म के ‘‘अद्-दीन'' होने का विश्वास आप प्राप्त कर लें और उस पर आप ईमान ले आएँ तो अनिवार्यतः उसको आपके जीवन के समस्त विभागों का धर्म होना चाहिए। यदि वह व्यक्तिगत रूप से आपका धर्म है तो कोई कारण नहीं कि वही आपके घर का भी धर्म न हो, आप की सन्तान की शिक्षा और आपकी पाठशाला का, आप के व्यवहार का और जीविका-उपार्जन का, आपके सामाजिक जीवन का एक और राष्ट्रीय कार्य-प्रणाली का, आपकी संस्कृति और राजनीति का, आपके साहित्य और कला का धर्म भी न हो, जिस प्रकार यह बात असम्भव है एक-एक मोती अपनी-अपनी जगह तो मोती हो किन्तु माला की डोर में बहुत-से मोती पिरोए हों तो सब मिलकर चने के दाने बन जाएँ, इसी प्रकार यह बात भी मेरे मस्तिष्क को अपील नहीं करती कि व्यक्तिगत रूप से तो हम एक धर्म के मानने वाले हों किन्तु जब अपने जीवन को व्यवस्थित करें तो उस व्यवस्थिति-जीवन का कोई पक्ष उस धर्म के आज्ञापालन से वंचित रह जाए।
इन सब से बढ़कर, ईश्वर पर विश्वास की महत्वपूर्ण मांग यह है कि जिस धर्म के ‘‘अद्-दीन'' (धर्म-विशेष) होने पर आप ईमान लाएँ उसके लाभों से अपनी समस्त मानव-जाति का लाभ पहुँचाने की चेष्टा करें, और आपकी समस्त चेष्टा और प्रयास का केन्द्र और धुरी यह हो कि यही ‘‘अद्-दीन'' समस्त संसार का धर्म बन जाए। जिस प्रकार सत्य की प्रकृति यह है कि वह सत्तारूढ़ होकर रहना चाहता है, इसी प्रकार सत्य-वादिता की भी यह मुख्य प्रकृति है कि वह सत्य को जान लेने के बाद असत्य पर उसका प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा किए बिना चैन नहीं ले सकती। जो व्यक्ति देख रहा हो कि असत्य हर ओर पृथ्वी और उसके निवासियों पर छाया हुआ है और फिर यह दृश्य उसके अन्तर में कोई विकलता, चुभन, कोई तड़प उत्पन्न नहीं करता, उसके हृदय में यदि सत्यवादिता है भी तो साई हुई है। उसे चिन्ता करनी चाहिए कि निद्रा की निश्चलता कहीं मृत्यु की निश्चलता में परिवर्तित न हो जाए।
----------------------------
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe Bi-Weekly E-Newsletter:
HindiIslamMail@gmail.com
Subscribe Our You Tube Channel
https://www.youtube.com/c/hindiislamtv
----------------------------
ऊपर पोस्ट की गई पुस्तिका ख़रीदने के लिए संपर्क करें:
MMI Publishers
D-37 Dawat Nagar
Abul Fazal Enclave
Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 011-26981652, 011-26984347
Mobile: +91-7290092401
https://www.mmipublishers.net/
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
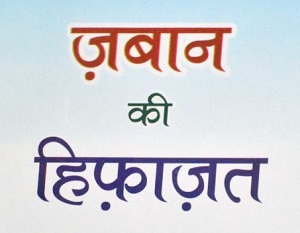
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
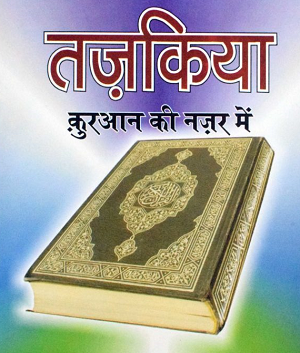
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

