
इस्लाम का नैतिक दृष्टिकोण
-
इस्लाम
- at 30 May 2022
मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी
अनुवादक: अफ़ज़ल हुसैन एम. ए.
प्रकाशक: मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स (MMI Publishers) नई दिल्ली
साधारण अवस्था में जबकि जीवन-सरिता शांतिपूवर्क बह रही हो, मनुष्य एक प्रकार का सन्तोष अनुभव करता है, क्योंकि ऊपर का स्वच्छ धरातल एक आवरण बन जाता है जिसके नीचे तह में बैठी हुई गन्दगियाँ और मलतत्व छिपे रहते हैं और आवरण की बाह्य स्वच्छता मनुष्य को इस बात का अनुसंधान करने की आवश्यकता कम ही अनुभव होने देती है कि तह में क्या कुछ छिपा हुआ है? परन्तु जब इस नदी में तूफ़ान उठता है, और उथल-पुथल के कारण नीचे की छिपी हुई सारी गन्दगियाँ उभर कर प्रकट रूप में नदी के धरातल पर बहने लगती हैं, उस समय अन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके नेत्रों में कुछ भी आलोक शेष है, साफ़-साफ़ देख लेता है कि जीवन-सरिता यह कुछ अपने भीतर लिये हुए चल रही है और यही वह समय होता है जब साधारण मनुष्यों में इस आवश्यकता की अनुभूति उत्पन्न हो सकती है कि उस उद्गम का पता लगायें जहां से जीवन-सरिता में यह गन्दगियाँ आ रही हैं, और उस उपाय की खोज करें जिससे इस सरिता को स्वच्छ किया और रखा जा सके। परन्तु यदि ऐसी अवस्था में भी लोग इस आवश्यकता का अनुभव न करें तो यह इस बात का लक्षण है कि मानव-जाति प्रमाद के नशे में चूर, लाभ-हानि से सर्वथा निश्चित हो चुकी है।
वर्तमान काल जिसमें हम आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं कुछ इन्हीं असाधारण परिस्थितियों का काल है। जीवन-सरिता इस समय चढ़ाव पर है। देशों, राष्ट्रों तथा जातियों के बीच घोर संघर्ष पाया जाता है और इस संघर्ष की जड़ें इतनी गहराई तक उतरी हुई हैं कि बड़े-बड़े समूहों की क्या चर्चा, व्यक्तियों तक को रणस्थल में खींच लाई है। इस प्रकार मानव मात्र के बहुत बड़े अंग ने अपने वे समस्त नैतिक अवगुण उगलकर सर्वसाधारण के सम्मुख रख दिये हैं जिन्हें वह युगों से भीतर ही भीतर पाल रहा था। अब हम इन गन्दगियों को जीवन के धरातल पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं जिनकी खोज के लिये पहले कुछ न कुछ गहराई तक उतरने की आवश्यकता थी। अब केवल कोई जन्मांध ही इस भ्रम में पड़ा रह सकता है कि "बीमार का हाल अच्छा है", और केवल वही लोग चिकित्सा की ओर से असावधान रह सकते हैं जो पशुओं के समान नैतिक अनुभूति से सर्वथा वंचित हैं या जिनकी नैतिक अनुभूति नष्ट हो चुकी है।
हम देख रहे हैं कि पूरे-पूरे राष्ट्र विस्तृत रूप से उन अति घृणित नैतिक अवगुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको सदैव से मानवता की अन्तरात्मा अत्यन्त घृणास्पद समझती रही है। अन्याय, क्रूरता, निर्दयता, अत्याचार, झूट, छल-कपट, मिथ्या, भ्रष्टाचार, निर्लज्जता, वचन-भंग, काम-पूजा, बलात्कार और ऐसे ही अन्य अभियोग केवल व्यक्तिगत अभियोग नहीं रहे हैं अपितु राष्ट्रीय आचरण एवं नीति का रूप धारण कर चुके हैं। संसार के बड़े-बड़े राष्ट्र सामूहिक रूप से वह सब कुछ कर रहे हैं जिनके करने वाले अभियुक्त अभी तक उनके यहाँ जेलों में ठूंसे जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र ने छाँट-छाँटकर अपने बड़े से बड़े अपराधियों को अपना लीडर और नेता बनाया है और बड़े से बड़ा पाप ऐसा नहीं रह गया है जो उनके नेतृत्व में अति निर्लज्जता के साथ बड़े पैमाने पर खुल्लम-खुल्ला न हो रहा हो। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति झूट गढ़-गढ़ कर पूरी ढिठाई से प्रकाशित कर रहा है और रेडियो द्वारा इन मिथ्या भाषणों से वायु मण्डल तक को गन्दा कर दिया है। पूरे-पूरे देशों तथा महाद्वीपों की जनसंख्यायें लुटेरों और डाकुओं में परिवर्तित हो गई हैं और प्रत्येक डाकू ठीक उस समय जब कि वह स्वयं डाका डाल रहा होता है अत्यन्त निर्लज्जता से अपनी विरोधी के डाके की निन्दा करता है और उस पर हाहाकार मचाता है यद्यपि स्वयं उसका अपना माथा भी अपने विरोधी से कुछ कम कलंकित नहीं होता। इन अत्याचारियों के निकट न्याय का अर्थ केवल अपने राष्ट्र के साथ न्याय करना रह गया है। स्वत्व जो कुछ है उनके लिए है, दूसरे के अधिकारों पर हाथ डालना उनके नीति-शास्त्र में न केवल उचित अपितु शुभ-कृत्य है। लगभग समग्र राष्ट्रों की दशा यह हो चुकी है कि उनके यहाँ लेने के बाट और हैं देने के और। जितने मापदण्ड वह अपने स्वार्थ तथा लाभ के निमित्त स्थिर करते हैं, दूसरों का लाभ सामने आते ही वे सारे मापदण्ड रूपान्तरित हो जाते हैं। जिन नियमों के पालन की वे दूसरों से आशा रखते हैं उनका पालन स्वयं करना निषिद्ध समझते हैं। वचन-भंग का रोग उस प्राकाष्ठा को प्राप्त हो चुका है कि अब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर कोई विश्वास नहीं रहा। बड़े-बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि अत्यन्त सभ्य रूप धारण किये हुये जब अन्तर्राष्ट्रीय संघों पर हस्ताक्षर कर रहे होते हैं उस समय उनके हृदय में यह दुःसंकल्प छिपा हुआ होता है कि पहला अवसर मिलते ही इस पवित्र बकरे को राष्ट्रीय स्वार्थ के थान पर भेंट चढ़ावेंगे; और जब एक राष्ट्र का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस बलिदान के लिए छुरी तेज़ करता है तो अखिल राष्ट्र में से एक आवाज़ भी इस कुनीति के विरुद्ध नहीं उठती, अपितु देश की सारी जनसंख्या इस अपराध में सम्मिलित हो जाती है। छल कपट तथा कूटनीति का हाल यह है कि बड़े-बड़े पवित्र नैतिक सिद्धान्तों की बात केवल इसलिए की जाती है कि संसार को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा किया जाये, और सीधे-सादे मनुष्यों को विश्वास दिलाया जाय कि तुम से जनधन के बलिदान की माँग जो हम कर रहे हैं यह कुछ अपने लिये नहीं है बल्कि हम नि:स्वार्थी, शुभचिंतक आत्म-त्यागी, तथा नेकों के नेक लोग यह सारा कष्ट केवल मानवता की भलाई के लिए उठा रहे हैं। निर्दयता एवं क्रूरता उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है कि एक देश जब दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसकी जनसंख्या को रौदने और कुचलने में केवल स्टीमरोलर की सी स्पन्दनहीनता ही उससे प्रकट नहीं होती अपितु वह बहुत मज़े ले-ले कर संसार को अपने इन कृत्यों से अवगत कराता है मानो उसे विश्वास है कि अब संसार में मनुष्य नहीं अपितु केवल भेड़िये बसते हैं। स्वार्थपूर्ण क्रूरता उस पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने स्वार्थ के लिए जीतकर अपना अधीन बना चुकने के पश्चात् केवल यही नहीं कि निर्दयता तथा निष्ठुरता के साथ उसे लूटता-खसोटता है अपितु क्रमबद्ध रूप से अनंत प्रयत्न करता रहता है कि मनुष्यता के समस्त सद्गुणों से उसको वंचित करके उसमें वे सारे दुर्गुण भर दे जिन्हें वह स्वयं अत्यन्त घृणास्पद समझता है।
यह कतिपय प्रत्यक्ष नैतिक अवगुणों का मैंने केवल उदाहरण स्वरूप उल्लेख किया है, अन्यथा यदि विस्तार से अनुसंधान किया जाय तो ज्ञात होगा कि पूरी मानवता का शरीर नैतिक दृष्टि से सड़ गया है। पहले व्यभिचार तथा जुये के अड्डे ही नैतिक पतन के सबसे बड़े फोड़े समझे जाते थे किन्तु अब तो हम जिधर देखते हैं मानव संस्कृति पूरी की पूरी एक फोड़ा ही दिखाई दे रही है। राष्ट्रों की पार्लियामेन्ट तथा असेम्बलियाँ, शासनों के सिक्रेटरियेट तथा मन्त्रिमण्डल, न्यायालय तथा वकालतख़ाने, प्रेस और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, यूनिवर्सिटियाँ तथा शिक्षा संस्थायें, बैंक और औद्योगिक एवं व्यापारिक व्यवसाय के अड्डे सब के सब फोड़े ही फोड़े हैं जो किसी तेज़ नश्तर की मांग कर रहे हैं। सबसे अधिक शोचनीय बात तो यह है कि ज्ञान-विज्ञान जो मानवता का प्रियतम तथा बहुमूल्य रत्न है आज इसका प्रत्येक विभाग मानवता के विनाश के निमित्त प्रयुक्त हो रहा है। शक्ति तथा जीवन के समस्त साधन जो प्रकृति ने मनुष्य के लिये एकत्र किये थे, उपद्रव तथा बिगाड़ के कामों पर लगाकर नष्ट किये जा रहे हैं, और वे सद्गुण भी जो मनुष्य के श्रेष्ठतम नैतिक गुण समझे जाते थे जैसे वीरता, त्याग, बलिदान, उदारता, सहानुभूति, धैर्य, नि:स्वार्थपरता, सहन-शीलता, दृढ़संकल्प, उच्चोत्साह आदि आज उनको भी कुछ बड़े तथा मौलिक दुर्गुणों का दास बनाकर रख दिया गया है।
विदित है कि सामूहिक अवगुण उस समय उभरकर सामने आते हैं जब वैयक्तिक अवगुण अपनी चरम सीमा को पहुंच चुके होते हैं। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समाज के अधिकांश व्यक्ति सदाचारी हों और वह समाज सामूहिक दुराचार का प्रदर्शन करे। यह किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है कि सदाचारी तथा भलेमानस लोग अपना नायकत्व, प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व दुराचारियों के हाथ में दे दें और इस बात पर सहमत हो जायें कि उनके जातीय, राष्ट्रीय, एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषय अनैतिक सिद्धान्तों पर चलाये जायें। इसलिए बड़े पैमाने पर संसार के राष्ट्र इन घृणास्पद नैतिक अवगुणों का प्रदर्शन अपनी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आज मानव जाति अपनी समस्त वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के होते हुए एक घोर नैतिक पतन का ग्रास है और इसके अतिरिक्त व्यक्ति इससे प्रभावित हो चुके हैं। यह परिस्थित यदि यों ही प्रगतिशील रही तो वह समय दूर नहीं जब मानवता किसी महाविनाश से दो-चार होगी और एक विशाल अधिकार उस पर छा जायगा।
अब यदि हम आँखें बन्द करके विनाश के गड्ढे की ओर सरपट जाना नहीं चाहते तो हमें खोज लगानी चाहिए कि इस बिगाड़ का उद्गम कहां है जहां से यह तूफ़ान के समान उमड़ा चला आ रहा है। चूंकि यह नैतिक पतन है अत: निस्संदेह हमें इसका पता उन नैतिक कल्पनाओं ही में मिलेगा जो इस समय संसार में प्रचलित है।
संसार की नैतिक कल्पनायें क्या हैं? इस प्रश्न का जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आधारत: यह समस्त कल्पनायें दो बड़े भागों में विभाजित हैं।
एक प्रकार की कल्पनायें वे हैं जो ईश्वर और मरणोत्तर जीवन के धार्मिक विश्वास पर आश्रित हैं।
दूसरे प्रकार की कल्पनायें वे हैं जो धार्मिक विश्वासों से पृथक किसी अन्य आधार पर अवलम्बित होती हैं।
आइये अब हम इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं की जांच पड़ताल करके देखें कि संसार में इस समय यह किस रूप में पाई जाती हैं और उनके परिणाम क्या हैं?
ईश्वर तथा मरणोत्तर जीवन के धार्मिक विश्वास पर जितनी नैतिक कल्पनायें स्थिर होती हैं उनके रूप में पूर्ण अवलम्बन उस विश्वास की प्रकृति पर होता है जो ईश्वर तथा मरणोत्तर जीवन के विषय में लोगों में पाया जाता है। अतएव हमें देखना चाहिये कि संसार इस समय ईश्वर को किस रूप में मान रहा है और मरणोत्तर जीवन के सम्बन्ध में उसकी सामान्य धारणायें क्या हैं।
ईश्वर को मानने वाले अधिकतर मनुष्य इस समय अनेकेश्वरवाद में लीन हैं उन्होंने अपने विचार में ईश्वरत्व के बहुत से अधिकार, विशेषतया वे अधिकार जिनका सम्बन्ध उनके अपने जीवन से है, अन्य सत्ताओं पर विभाजित कर दिये हैं और सत्ताओं की काल्पनिक आकृति अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी बना ली है कि वह अपने इन ईश्वरीय अधिकारों को ठीक उसी प्रकार प्रयोग करता है जिस प्रकार ये चाहते हैं कि वह प्रयोग करें। ये पाप करते हैं वह क्षमा तथा मोक्ष प्रदान कर देती है। ये कर्तव्य की ओर से असावधान और अधिकार की ओर से विमुख होकर बिना नाथ के बैल की तरह वैध अवैध तथा उचित अनुचित में अन्तर किये बिना संसार की खेती को चरते-फिरते हैं और वे कुछ चढ़ावे के बदले उनके निर्वाण की ज़मानत ले लेती है। ये चोरी भी करने जाते हैं तो उनकी कृपा से थानेदार सोता रह जाता है। इनके और उनके बीच यह सौदा पट जाता है कि ये उनमें विश्वास एवं श्रद्धा रखें और चढ़ावे चढ़ाते रहें और उसके बदले में वे उनके सब काम, जो कुछ भी यह करना चाहें, बनाती रहेंगी और मरने के बाद जब ईश्वर उन्हें पकड़ना चाहेगा तो वे बीच में बाधक होकर कह देंगी कि ये हमारी शरण में हैं इनसे कुछ न कहा जाय। बल्कि किसी-किसी स्थान पर तो इस पकड़-धकड़ की नौबत ही न आयेगी, क्योंकि इनके पापों का प्रायश्चित पहले ही कोई कर चुका होगा। इन अंधविश्वासों तथा अनुचित श्रद्धाओं ने मरणोत्तर जीवन के धार्मिक विश्वास को भी निरर्थक कर दिया है और इसका परिणाम यह है कि वे समस्त नैतिक आधार खोखले हो चुके हैं जो धर्म ने निर्मित किये थे। धर्म संस्कार तथा नैतिकता की बातें पुस्तकों में लिखी हुई मौजूद हैं और मुँह से उनका उच्चारण भी आदर के साथ होता है परन्तु व्यवहार में उनके पालन से बचने के लिये बहुदेववाद ने अगणित राहें खोल दी हैं और कुछ इस रूप में खोली हैं कि जिस राह से भी चाहें जायें। प्रत्येक अवस्था में इन्हें विश्वास है कि अन्त में पहुंचेंगे मोक्ष ही के अभीष्ट स्थान पर।
बहुदेववाद को तो छोड़िये, जहां ईश भक्ति तथा मरणोत्तर जीवन का धार्मिक विश्वास कुछ अच्छे रूप में पाया जाता है वहां भी हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्यों की सूची सिकुड़ कर मानव जीवन के एक अतिसंकीर्ण वृत्त में सीमित हो गई है। कुछ संस्कार कुछ धार्मिक प्रथायें और कुछ प्रतिबन्ध हैं जिनकी सीमित व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में ईश्वर उनसे मांग करता है। और इन्हीं के बदले में उसने एक अति-विशाल बैकुण्ठ उनके लिये उपस्थित कर रखा है। यदि ये उन मांगों को पूरा कर दें तो फिर कोई चीज़ ईश्वर की ओर से उनके लिये करने की नहीं रह जाती, इसके बाद ये स्वतंत्र हैं कि अपने जीवन के सारे काम जिस प्रकार चाहें चलायें, और यदि इन ईश्वरीय मांगों में भी कोताही हो जाय तो उसकी कृपा एवं दया पर भरोसा है कि वह पापों की गठरी इनसे बैकुण्ठ के द्वार पर रखवा लेगा और अन्दर जाने के लिये टिकट निःशुल्क प्रदान कर देगा। इस संकीर्ण धार्मिक कल्पना ने एक तो जीवन के विभिन्न विषयों पर धर्मनीति के प्रभाव को अति सीमित कर दिया है, जिसके कारण जीवन के समस्त प्रमुख विभाग प्रत्येक उस नैतिक नेतृत्व, नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध से सर्वथा मुक्त हो गये हैं जो धर्म की अनिवार्य अपेक्षा थी, दूसरे इस संकीर्ण क्षेत्र में भी नैतिकता की पकड़ से बच निकलने के लिये एक मार्ग यहां खुला हुआ है जिससे लाभ उठाने में कम ही लोग सुस्ती दिखाते हैं।
इन सबसे अच्छी दशा जिन धार्मिक वर्गों की है, जो बहुदेववाद से भी सुरक्षित हैं और मरणोत्तर जीवन के सम्बन्ध में भी किसी झूठे भरोसे पर आश्रय नहीं कर बैठते हैं, उनके भीतर आचार व्यवहार की पवित्रता तो निस्सन्देह पाई जाती है और अतिसुन्दर व्यवहार तथा आचरण के लोग इनमें मिल जाते हैं, परन्तु इनको साधारणतः धर्म एवं आध्यात्मिकता की सीमित कल्पना ने बिगाड़ रखा है। वे संसार और इसकी जीवन-समस्याओं से बड़ी हद तक अलग-थलग होकर या तो कुछ विशिष्ट कृत्यों को जिन्हें धार्मिक कृत्य समझा जाता है, ले बैठते हैं, या अपनी आत्मा को माँझ-माँझकर स्वच्छ करते हैं ताकि वह इस संसार में ही परोक्ष लोक की वाणी सुनने तथा परम सौन्दर्य की छाया देखने के योग्य हो जायें। इनके विचार में मोक्ष का मार्ग ऐहिक जीवन के किनारे-किनारे बचकर निकल जाता है और ईश्वर-प्राप्ति से सुशोभित होने का उपाय बस यह है कि एक ओर धर्म के दिये हुये मानचित्र पर अपने जीवन के बाह्य पक्षों को ढाल लिया जाय, दूसरी ओर आत्मा के शुद्धीकरण की कुछ विधियों से काम लेकर उसे उज्जवल तथा प्रकाशमान कर दिया जाय, और फिर एक सीमित परिधि के भीतर कुछ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कृत्यों में व्यस्त रह कर जीवन के दिन पूरे कर दिये जायँ, मानो इनके ईश्वर को कुछ सुडोल शीशों के बर्तन, कुछ अच्छे लाउडस्पीकर, कुछ सुन्दर ग्रामोफून, कुछ कोमल रेडियो सेट, कुछ रोचक फोटो के केमरे चाहिये थे और इसी आशय से उसने इतनी कुछ सामग्री देकर मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा ताकि यहाँ से अपने आप को इन वस्तुओं में रुपान्तरित करके फिर उसके पास वापस पहुंच जायें। धर्म एवं आध्यात्मिकता की इस अशुद्ध कल्पना की सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि जो व्यक्ति शिष्टाचारी एवं पुण्यात्मा थे उन्हें यह ज्ञान ध्यान के लिये जीवन-क्षेत्र से हटाकर एकान्त में ले गई और संसार का कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचारी तथा पतित व्यक्तियों के लिये बिना बाधा के स्वत: रिक्त हो गया।
संसार की समस्त धार्मिक अवस्था का यह सारांश है और इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि ईश-भक्ति से जो नैतिक शक्ति मनुष्य को मिलनी सम्भव थी, अधिकतर मनुष्य तो उसे सर्वथा प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं और एक अति अल्पसंख्या इसको प्राप्त कर रही है परन्तु मानवता के नेतृत्व से उसने स्वयं हाथ खींच लिया है, इसलिये इसकी दशा उस बैट्री की सी है जिसमें बिजली भरी जाय और वह यों ही रखे अपनी आयु पूरी कर दे।
मानव-संस्कृति की गाड़ी व्यवहारत: जो लोग इस समय चला रहे हैं उनके नीतिशास्त्र ईश्वर तथा मरणोत्तर-जीवन की आधारभूत कल्पनाओं से रिक्त हैं और जान बूझकर रिक्त किये गये हैं, तथा नीति में ईश्वर के आदेश स्वीकार करने से उन्होंने सर्वथा इंकार कर दिया है। यद्यपि उनकी बहुत बड़ी संख्या किसी न किसी मत की मानने वाली है, परन्तु उनके विचार में धर्म प्रत्येक मनुष्य का एक वैयक्तिक विषय है जिसे मनुष्य को अपने व्यक्तित्व तक सीमित रखना चाहिये। जब सामाजिक जीवन तथा उसकी समस्याओं एवं पारस्परिक व्यवहारों से धर्म को कोई सम्बन्ध ही नहीं है, फिर इसकी क्या ज़रूरत कि वे इन विषयों को चलाने के लिये किसी अलौकिक आदेश के आकांक्षी बनें। गत शताब्दी के अन्त में जिस नैतिक आन्दोलन का आरम्भ अमरीका से हुआ था और जो बढ़ते-बढ़ते इंग्लैंड और दूसरे देशों में फैल गया, उसका आधारभूत मत American Ethical Union के उद्देश्य की सूची में इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था:_
"मानव-जीवन के समस्त सम्बन्धों में चाहे वे वैयक्तिक हों, सामाजिक हों, राष्ट्रीय हों या अन्तर्राष्ट्रीय, नीति के परम महत्व पर ज़ोर देना, बिना इसके कि धार्मिक विश्वासों अथवा अलौकिक कल्पनाओं का इसमें कोई प्रवेश हो।"
इस आन्दोलन से प्रभावित होकर इंग्लैंड में Union of Ethical Societies स्थापित हुई जो आगे चलकर इसी में सम्मिलित हो गई। इसका मौलिक उद्देश्य यह ठहराया गया था:-
"मानव हितैषिता और सेवा की एक ऐसी शैली का उपदेश देना जो इस सिद्धान्त पर अवलंबित हो कि धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य भलाई का प्रेम है और यह कि नैतिक कल्पनाओं तथा नैतिक जीवन के लिये संसार की वास्तविकता और मरणोत्तर-जीवन के सम्बन्ध में किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है और यह कि विशुद्ध मानुषिक एवं प्राकृतिक साधनों से मनुष्य को अपने समस्त जीवन-सम्बन्धों में सत्य से प्रेम करने, सत्य जानने और सत्य को प्रयोग में लाने के लिये तैयार किया जाये।"
इन शब्दों में वस्तुत: उस सम्पूर्ण वर्ग के विचार एवं भाव प्रकट किये गये हैं जो इस समय चिन्तन, सभ्यता संस्कृति, पारस्परिक व्यवहारों तथा अन्य विषयों में संसार का नेतृत्व कर रहा है। आज संसार के कारोबार को व्यवहारिक रूप से जो लोग चला रहे हैं उन सबके मस्तिष्क पर वही कल्पना छाई हुई है जो ऊपर के इन वाक्यों में प्रकट की गई है। व्यवहारत: सभी ने अपने नीति-शास्त्र को ईश्वर तथा मरणोत्तर जीवन पर विश्वास और धर्म के नैतिक पथ-प्रदर्शन से सर्वथा मुक्त कर लिया है। अब हमें उन नैतिक दर्शन-शास्त्रों का जिन्हें धर्म से मुक्त होकर उन्होंने अङगीकृत किया है, सिंहावलोकन करके देखना चाहिये कि इनकी क्या दशा है।
नीतिशास्त्र का प्रथम मौलिक प्रश्न यह है कि वह यथार्थ एवं सर्वश्रेष्ठ भलाई क्या है जिसको पहुँचना मानव चेष्टा एवं प्रयास का लक्ष्य होना चाहिए और जिसकी कसौटी पर मनुष्य की कार्यनीति को परख कर निर्णय किया जाय कि वह अच्छी है या बुरी, शुद्ध या अशुद्ध?
इस प्रश्न का कोई एक उत्तर मनुष्य नहीं पा सका। इसके बहुत से उत्तर हैं। एक वर्ग के निकट वह भलाई आनन्द है, दूसरे के निकट उत्कर्ष है, तीसरे के निकट "कर्त्तव्य के हेतु कर्तव्य" है।
फिर आनन्द के विषय में विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि कैसा आनन्द? क्या वह जो भोग विलास अथवा काम-सम्बन्धी अभिलाषाओं की पूर्ति से प्राप्त होता है? या वह जो मानसिक उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ने से प्राप्त होता है? या वह जो अपने व्यक्तित्व को आर्ट या आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से सुसज्जित कर लेने से प्राप्त होता है? और यह कि किस का आनन्द क्या प्रत्येक व्यक्ति का आनन्द? या उस समूह का आनन्द जिससे मनुष्य सम्बन्धित है? या समस्त मानव जाति का आनन्द? या तात्पर्य यह कि दूसरों का आनन्द?
इसी प्रकार उत्कर्ष को लक्ष्य नियत करने वालों के लिए भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उत्कर्ष की कल्पना और इसका मापदण्ड क्या है? और उत्कर्ष किसका लक्ष्य है? व्यक्ति का? समूह का? या मानव जाति का?
इसी प्रकार जो लोग "कर्तव्य के हेतु कर्तव्य" के क़ायल हैं और एक निरपेक्ष विधि (Categorical Imperative) के बिना ननुनच आज्ञापालन ही को अंतिम एवं उच्चतम भलाई समझते हैं, उनके लिये भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह विधि वास्तव में क्या है? किसने उनको बनाया है। और किस की विधि होने के नाते उसका पालन अनिवार्य है?
इन समस्त प्रश्नों का उत्तर विभिन्न समूहों के निकट विभिन्न है? केवल दर्शन शास्त्र की पुस्तकों ही में विभिन्न नहीं है अपितु प्रयोग तथा व्यवहार में भी विभिन्न हैं। यह मनुष्य की सारी भीड़ जो आपके सम्मुख मानव संस्कृति की गाड़ी को चला रही है जिसमें शासनों को चलाने वाले मंत्री, सेनाओं को लड़ाने वाले सेनापति, मनुष्यों के बीच निर्णय करने वाले न्यायाधीश, मनुष्य के पारस्परिक व्यवहारों के लिये नियम बनाने वाले शास्त्र-नियामक, नव-युवकों को तैयार करने वाले अध्यापकगण, मनुष्य के आर्थिक साधनों को कण्ट्रोल करने वाले कारोबारी लोग, और समाज के कार्यालय में काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ता, सब ही सम्मिलित हैं। इनके पास भलाई का कोई एक मापदण्ड नहीं है अपितु प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक समूह अपना अलग मापदण्ड रखता है और एक समाज-व्यवस्था में काम करते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति का मुख एक पृथक लक्ष्य की ओर फिरा हुआ है। किसी के समीप अपना आनन्द सब कुछ है और आनन्द से उसका तात्पर्य भौतिक अथवा काम वासनाओं की पूर्ति है। कोई अपने आनन्द के पीछे पड़ा हुआ है और उससे उसके मस्तिष्क में कुछ और ही आशय है। इस वैयक्तिक आनन्द की प्राप्ति तथा अप्राप्ति ही की दृष्टि से वह निर्णय कर रहा है कि सामाजिक जीवन में उसके लिये कौन सी व्यवहार-नीति अच्छी है या बुरी, किन्तु उसके बाह्य-सभ्य स्वरूप से हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव समाज के लिये वह एक उचित मंत्री, या न्यायाधीश, या अध्यापक, या किसी अन्य स्थिति में समाज की मशीन का एक अच्छा पुर्ज़ा है। इसी प्रकार कोई आनन्द का अर्थ मनुष्यों के उस विशेष वर्ग का आनन्द एवं समृद्धि समझता है जिसके साथ उसका सुख दु:ख तथा रुचि-सम्बद्ध है और यही उसके समीप वह परम पुण्य है जिसकी प्राप्ति की चेष्टा करना उसके निकट सदाचार है। यह दृष्टिकोण उसे अपने वर्ग या अपनी जाति के अतिरिक्त हर एक के लिये साँप और बिच्छू बना देता है किन्तु हम उसके बाह्य सभ्य-स्वरूप के कारण उसे एक सज्जन मनुष्य समझ लेते हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के व्यक्ति उत्कर्ष को सर्वोत्तम भलाई मानने वालों और "कर्तव्य के हेतु कर्त्तव्य" के मानने वालों में पाये जाते हैं, जिनमें से बहुत-सों के सिद्धान्त अपने व्यावहारिक परिणामों की दृष्टि से मानव-संस्कृति एवं सभ्यता के लिये विष की विशेषता रखते हैं परन्तु वह अमृत का लेबल लगाये हमारे सामाजिक जीवन में सम्मिलित हुए चले जा रहे है।
अब आगे चलिये। नीति-शास्त्र के मौलिक प्रश्न में से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे पास पाप-पुण्य जानने का साधन क्या है? किस मूलाधार अथवा स्रोत की ओर हम यह जानने के लिये रुख़ करें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या?
इस प्रश्न का कोई एक उत्तर मनुष्य को नहीं मिला। इसके भी बहुत से उत्तर हैं। किसी के निकट वह साधन और मूलाधार मानवता का अनुभव है, किसी के निकट प्राकृतिक नियम, और अस्तित्व की अवस्थाओं का ज्ञान है, किसी के निकट भावरस (Sentument) है किसी के निकट बुद्धि एवं विवेक है। यहां पहुंच कर वह विशृंखलता अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती है जिसका आपने प्रथम प्रश्न के विषय में निरीक्षण किया है। इन वस्तुओं को मूलाधार नियत करने के बाद नैतिकता के लिये स्थाई सिद्धांत ही यह स्थिर हो जाता है कि इसका कोई निश्चित माप-दण्ड न हो अपितु वह एक द्रव पदार्थ के समान बहता और विभिन्न आकृतियों तथा माप-पत्रों में ढलता चला जाय।
मानवता के अनुभवों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है कि उस के विषय में सम्पूर्ण तथा विस्तृत जानकारियाँ एक स्थान पर एकत्र हों और कोई सर्वदर्शी एवं सर्वत्र तथा परम संतुलित मस्तिष्क इनसे विवेचना करके फल निकाले; परन्तु इसका अभाव है। एक तो मानवता का अनुभव अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अपितु चल रहा है, फिर अब तक का जो अनुभव है उसके भी विभिन्न अंश लोगों के सम्मुख हैं और वह विभिन्न रूप से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार इनसे फल निकाल रहे हैं, तो क्या इन अपूर्ण जानकारियों से विभिन्न दोषयुक्त मस्तिष्क अपनी रुचि के अनुसार जो फल भी निकाल लें वे सब शुद्ध हो सकते हैं? यदि नहीं, तो कैसे असाध्य रोगी हैं वे मस्तिष्क जो अपनी भलाई बुराई को जानने के लिये इस ज्ञानसाधन को पर्याप्त समझते हैं।
यही मामला प्राकृतिक-नियमों तथा अस्तित्व की अवस्थाओं का है। या तो आप नैतिक भलाई और बुराई को जानने के लिये उस समय की प्रतीक्षा करें जब इन नियमों और अवस्थाओं का ज्ञान संतोषजनक सीमा तक आपकी पकड़ में आ जाये या नहीं तो अपर्याप्त ज्ञान को अपर्याप्त जानते हुये इन्हीं के आधार पर विभिन्न मनोवृत्ति और विभिन्न योग्यता के लोग विविध प्रकार से निर्णय करते रहें कि उनके लिये भलाई क्या है और बुराई क्या, और ज्ञान की प्रत्येक नवीन अन्शिका प्राप्त होने के पश्चात इन निर्णयों को परिवर्तित भी करते रहें यहाँ तक कि आज की भलाई कल बुराई हो जाय और आज की बुराई कल भलाई मानी जाने लगे।
बुद्धि विवेक तथा भावरस का मामला भी इससे कुछ भिन्न नहीं है। निस्सन्देह पुण्य एवं पाप को जानने की योग्यता बुद्धि को भी प्राप्त है और इस बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य ने कुछ न कुछ भाग पाया है और भलाई बुराई का कुछ भावात्मक अंश भी है जिसका श्रुतिप्रकाशन (इलहाम) प्रत्येक मनुष्य की अन्तरात्मा पर स्वभावतः होता है परन्तु इस ज्ञान के लिये इनमें से कोई भी स्वपर्याप्त नहीं कि इसी को अन्तिम और एकमात्र ज्ञान साधन की स्थिति में ले लिया जाय। बुद्धि या भावरस जिसको भी आप स्वपर्याप्त समझें फिर भी एक ऐसे ज्ञान-साधन पर आज भरोसा करेंगे जो न केवल यह कि अपनी प्रकृति में अपूर्ण एवं सीमित है अपितु वह विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न युगों में पहुंचकर सर्वथा विभिन्न वस्तुओं पर पाप या पुण्य होने की व्यवस्था देता है।
यह सारी अव्यवस्था एवं विशृंखलता जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, केवल वैज्ञानिक निबन्धों एवं दार्शनिक विवादों तक ही सीमित नहीं अपितु वास्तव में संसार की सभ्यता एवं संस्कृति में व्यावहारतः इसकी छाया पूर्णरूपेण स्पष्ट हो रही है। आपकी संस्कृति में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वह कार्यकर्ता हों या कर्मचारी या कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों के बनाने में लगे हुये हों, ये सब पाप पुण्य तथा शुद्ध अशुद्ध जानने के लिये अपने अपने ढंग पर इन्हीं विभिन्न उद्गमों की ओर रुख़ कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समूह का पाप पुण्य से पृथक है यहाँ तक कि एक का पुण्य दूसरे का घोर पाप है और एक का पाप दूसरे का सर्वोत्तम पुण्य है। इस अव्यवस्था ने नीति के लिये कोई स्थाई एवं सुद्दढ़ मूलाधार शेष ही नहीं रहने दिया है। जिन चीज़ों को संसार सदैव से लज्जापूर्ण अनैतिकता समझता आया है या जिन्हें सदैव से अपराध एवं पाप समझा जाता रहा है आज किसी न किसी समुदाय की दृष्टि में वह निर्पेक्ष पुण्य नहीं तो सापेक्ष पुण्य बन गये हैं। इसी प्रकार जिन भलाइयों को सदैव से मनुष्य सद्गुण समझता रहा है उनमें से अधिकतर आज मूर्खता अथवा हास्य ठहराये जा चुके हैं और विभिन्न समूह इनका अतिक्रमण, लज्जा के साथ नहीं अपितु गर्व के साथ खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। पहले झूठा झूठ बोलता था परन्तु नैतिक मापदण्ड सच्चाई ही को मानता था किन्तु आज के दर्शनशास्त्रों ने झूठ को पुण्य बना दिया है और झूठ बोलने की एक नियमबद्ध कला सम्पादित की जा रही है और बड़े पैमाने पर जातियाँ तथा राष्ट्र झूठ फैला रहे हैं। यही दशा प्रत्येक अवगुण की है कि पहले अवगुण, अवगुण ही थे परन्तु आज नवीन दर्शनशास्त्रों की "कृपा' से वे सब निरपेक्ष या सापेक्ष सदाचार में परिवर्तित कर दिये गये हैं।
नीतिशास्त्र के मौलिक प्रश्नों में से तृतीय प्रश्न यह है कि नैतिक नियम के पीछे वह सत्ता कौन सी है जिसके बल पर ये नियम लागू हों। इसके उत्तर में आनन्द अथवा उत्कर्ष के पूजक कहते हैं कि आनन्द अथवा उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली भलाइयाँ अपना अनुवर्तन कराने की शक्ति आप रखती हैं और अपकर्ष एवं कष्ट तथा नीचता की ओर ले जाने वाली बुराइयाँ आप अपने ही बल पर अपने से दूर रखती हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक नियम के लिये किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता ही नहीं। दूसरा वर्ग कहता है कि कर्त्तव्य-परायणता का नियम मनुष्य के उचित संकल्प का अपने ऊपर आप लागू किया हुआ नियम है इसके लिये किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वर्ग राजसत्ता को नैतिक नियमों की वास्तविक नियामिका शक्ति समझता है और इस मत के अनुसार स्टेट को वे समस्त अधिकार मिल जाते हैं जो पहले ईश्वर के लिये थे अर्थात स्टेट की जनसंख्या के सम्बन्ध में यह निर्णय करना कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिए। चतुर्थ वर्ग ने यह स्थिति स्टेट के स्थान पर समाज की मानी है। यह सारे उत्तर बिगाड़ के असंख्य रूप संसार में व्यवहारत: उत्पन्न कर चुके हैं और अब तक कर रहे हैं। पहले दो उत्तरों ने व्यक्तिगत स्वेच्छाचार एवं पथभ्रष्टता यहां तक बढ़ा दिया कि सामूहिक जीवन अस्त-व्यस्त तथा अव्यवस्थित होने के समीप पहुंच गया। फिर इसकी प्रतिक्रिया उन दर्शनशास्त्रों के रूप में प्रकट हुई जिन्होंने या तो स्टेट को ईश्वर बनाकर व्यक्तियों को सर्वथा इसका दास बना डाला या फिर व्यक्तियों की रोटी के साथ उनके पाप पुण्य की बागडोर भी समाज के हाथों में दे दी यद्यपि पावन अथवा निर्दोष न स्टेट है न समाज।
यही मामला इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत होता है कि वह कौन-सा प्रेरक है जो मनुष्य को अपनी स्वाभाविक रुचि के होते हुये भी उसके प्रतिकूल नैतिक आदेशों के पालन पर तत्पर करे? किसी के निकट केवल आनन्द की लालसा और कष्ट का भय इसके लिये यथेष्ट प्रेरक है। कोई केवल निपुणता अथवा उत्कर्ष की इच्छा और दोष से सुरक्षित रहने की अभिलाषा को इसके लिये पर्याप्त समझता है। कोई इसके लिये केवल मनुष्य के उस मनोवेग पर भरोसा करता है जो उसे नियमों के अतिक्रमण से रोकता तथा उसके पालन पर उभारता है। कोई स्टेट के प्रतिदान की आशा और उसके कोप के भय को महत्व देता है और कोई समाज के प्रतिदान अथवा भय को।
इनमें से प्रत्येक उत्तर ने व्यवहारत: हमारी नैतिक व्यवस्थाओं में से किसी न किसी के भीतर प्रधानता का स्थान प्राप्त कर लिया है और थोड़ा सा अनुसंधान करने पर यह तथ्य सरलतापूर्वक स्पष्ट हो सकता है कि यह सब प्रेरक दुराचार के लिये भी उतने ही अच्छे प्रेरक हैं जितने सदाचार के लिये, अपितु इनमें दुराचार के लिये प्रेरक बनने की शक्ति अधिक है, और कुछ भी हो किसी उत्तम श्रेणी की नीति के लिये तो यह समस्त प्रेरक सर्वथा अपर्याप्त हैं।
यह अतिसंक्षिप्त सिंहावलोकन जो मैंने संसार की वर्तमान नैतिक अवस्था का किया है उससे एक दृष्टि में यह अनुभव हो जाता है कि संसार में इस समय एक विश्व-व्यापी नैतिक विशृंखलता पाई जाती है। ईश्वर से निःस्पृह तथा विमुख होकर मनुष्य कोई ऐसा आधार न पा सका जिस पर वह संतोष-जनक विधि से अपनी नैतिकता का निर्माण करता। नैतिकता के सारे मौलिक प्रश्न इसके लिये वस्तुत: समस्या बन कर रह गये जिनका कोई समाधान उसकी समझ में नहीं आता, न वह उस सर्वोत्तम भलाई का पता लगा सका, जो उसकी चेष्टाओं का शिरोबिन्दु बनने के योग्य होती और जिसके आधार पर व्यवहार तथा आचरण के बुरे भले, उचित अनुचित होने का निर्णय किया जा सकता, न उसे वह मूलाधार तथा उद्गम कहीं हाथ लगा जिससे वह शुद्ध रूप से ज्ञात कर सकता कि पाप क्या है और पुण्य क्या, न उसे वह नियामिका-शक्ति प्राप्त करने में सफलता हुई जिसको नैतिक आदेश (Sanction) से नीति के किसी श्रेष्ठ, सम्पूर्ण तथा सर्वव्यापी नियम को लागू करने की शक्ति प्राप्त होती, और न उसे कोई ऐसा प्रेरक मिल सका जो मनुष्य में सन्मार्ग पर चलने और कुमार्ग से बचने के लिये वास्तविक उत्तेजना उत्पन्न करने के योग्य होता। ईश्वर से विद्रोह करके मनुष्य ने स्वेच्छापूर्वक इन प्रश्नों को हल करना चाहा और अपने निकट हल किया भी, किन्तु यह उसी हल के उत्पन्न किये हुये परिणाम हैं जो आज हमको नैतिक पतन के एक भीषण तूफ़ान के रूप में उठते और पूरी मानव-सभ्यता को विनाश की धमकियाँ देते दिखाई दे रहे हैं।
क्या अब भी वह समय नहीं आया कि हम इस आधार का अनुसंधान करें जिस पर नीति का ठीक निर्माण हो सके? वस्तुत: यह अनुसंधान केवल एक ज्ञानात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रसंग नहीं है अपितु हमारे जीवन की एक व्यवाहारिक आवश्कयता है और समय की गम्भीरता ने इसको अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता बना दिया है। इसी विचार से मैं अपने अनुसंधान तथा छान-बीन का फल प्रस्तुत करता हूं और चाहता हूं कि जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव कर रहे हैं वे न केवल मेरे निष्कर्ष पर गम्भीरता पूर्वक एकाग्रचित से विचार करें वरन स्वयं भी सोचें कि मानव-नीति के लिये आख़िर कौन-सा आधार शुद्ध हो सकता है।
मैं अपने अनुसंधान तथा छान-बीन से जिस परिणाम पर पहुंचा हूं वह यह है कि नीति के लिये केवल एक ही आधार शुद्ध है और वह इस्लाम प्रस्तुत करता है। यहां नीति-शास्त्र के समस्त मौलिक प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाता है और ऐसा उत्तर मिलता है जिसके भीतर वह त्रुटियां विद्यमान नहीं हैं जो दार्शनिक (Philosophical) उत्तरों में पाई जाती हैं। यहाँ धार्मिक नीति-शास्त्रों की उन त्रुटियों में से भी कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है जिनके कारण वे न किसी दृढ़ चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और न मनुष्य को संस्कृति के विस्तीर्ण दायित्व के संभालने के योग्य बनाते हैं। यहाँ एक ऐसा सर्व-व्यापक नैतिक नेतृत्व प्राप्त होता है जो जीवन के समस्त विभागों में उन्नति की यथा-सम्भव उच्चतम श्रेणी तक हमें ले जा सकता है। यहाँ वे नैतिक सिद्धान्त हमें मिलते हैं जिन पर एक पवित्रतम समाज-व्यवस्था स्थापित हो सकती है और यदि इन सिद्धान्तों पर वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार की नींव रखी जाय तो मानव जीवन उस बिगाड़ से सुरक्षित रह सकता है जिससे वह इस समय दो चार है। इस परिणाम पर मैं किन युक्तियों द्वारा पहुंचा हूँ? इसकी संक्षिप्त व्याख्या मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।
दर्शनशास्त्र जिस स्थान से अपना नैतिक प्रसंग आरम्भ करता है वास्तव में वह नीति समस्या का सिरा नहीं है अपितु मध्य के कुछ बिन्दु है जिन्हें सिरे को छोड़ कर उसने आरम्भ-बिन्दु बना लिया है और यही उसकी प्रथम भूल है। यह प्रश्न कि मनुष्य के लिये आचरण की शुद्धि-अशुद्धि का मापदण्ड क्या है? और वह कौन-सी भलाई है जिसकी प्राप्ति का प्रयास मनुष्य के लिये वांछनीय होना चाहिये। वास्तव में यह बाद का प्रश्न है। इससे पहले जिस समस्या का समाधान होना चाहिये वह यह है कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति क्या है? इस प्रश्न को इसलिये समस्त प्रश्नों पर प्रधानता प्राप्त है कि स्थिति के निश्चय के बिना नैतिकता का प्रश्न केवल निरर्थक ही नहीं हो जाता अपितु इसमें प्राय: सम्भावना इसी बात की होती है कि इस प्रकार जो नैतिक सिद्धान्त नियत किये जायेंगे वे मूलत: अशुद्ध होंगे। उदाहरण स्वरूप किसी जायदाद के विषय में आपको यह निश्चित करना है कि इसमें किस प्रकार मुझे काम करना चाहिये और किस प्रकार के अधिकार मेरे लिये उचित हैं और किस प्रकार के अधिकार अनुचित। क्या आप इस प्रश्न को ठीक-ठीक हल कर सकते हैं जब तक कि इस बात को निश्चित न कर लें कि इस जायदाद में आपकी स्थिति क्या है? और इससे आपके सम्बन्ध की प्रकृति क्या है? यदि यह सम्पत्ति किसी दूसरे के आधिपत्य में है और आपकी स्थिति न्यासिक की-सी है तो आपके लिये इसमें नैतिक कार्यप्रणाली की प्रकृति कुछ और होगी और यदि आप स्वयं इसके अधिनायक हैं और इस पर आपके स्वामित्व-अधिकार असीम हैं तो आपके नैतिक व्यवहार की प्रकृति सर्वथा दूसरी हो जायेगी और बात केवल इतनी ही नहीं है कि स्थिति का प्रश्न नैतिक व्यवहार की प्रकृति के विषय में निर्णायक है अपितु वास्तव में इसी पर इस बात का निर्णय भी आश्रित है कि उस जायदाद में आपके लिये उचित व्यवहार-नीति निश्चित करने का अधिकारी कौन है, आप स्वयं या वह जिसके आप न्यासिक हैं।
इस्लाम सबसे पहले इसी प्रश्न की ओर ध्यान देता है और हमें सर्वथा स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से बताता है कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति ईश्वर के दास एवं प्रतिनिधि की है। यहाँ मनुष्य को जितनी वस्तुओं से सम्पर्क होता है वे सब ईश्वर की सम्पत्ति हैं, यहाँ तक कि मनुष्य का अपना शरीर और वह समस्त शक्तियाँ भी जो उस शरीर में भरी हुई हैं, मनुष्य की अपनी मिल्कियत नहीं हैं अपितु ईश्वर की मिल्कियत हैं ईश्वर ने इसको उन समस्त वस्तुओं में हस्तक्षेप का अधिकार देकर यहाँ अपने प्रतिनिधि की स्थिति में नियुक्त किया है और इस नियुक्ति में उसकी परीक्षा है। परीक्षा का अन्तिम फल इस संसार में नहीं निकलेगा, अपितु जब व्यक्तियों, जातियों तथा सम्पूर्ण मानव जाति का कृत्य समाप्त हो चुकेगा और मनुष्यों के प्रयास के प्रभाव एवं परिणाम पूर्णता को प्राप्त हो चुकेंगे, तब ईश्वर एक साथ इन सबकी पूछताछ करेगा और इस बात का निर्णय करेगा कि किसने उसकी भक्ति एवं प्रतिनिधित्व सम्बंधी कर्तव्यों का पालन ठीक-ठीक किया है और किसने नहीं किया। यह परीक्षा किसी एक विषय में नहीं अपितु समग्र विषयों में है, किसी एक जीवन-विभाग में नहीं वरन् सामूहिक रूप से पूर्ण जीवन में है। मन एवं मस्तिष्क तथा आत्मा एवं शरीर की जितनी शक्यिाँ मनुष्य को दी गई हैं सबकी परीक्षा है, और बाह्य में जिन-जिन वस्तुओं पर जिस-जिस प्रकार के अधिकार उसे प्रदान किये गये हैं उन सब में भी परीक्षा है कि वह किस प्रकार इन पर अपना अधिकार प्रयोग में लाता है।
स्थिति की इस नियति का तर्कसंगत फल यह है कि संसार में अपने लिए नैतिक व्यवहार की नियति का अधिकार ही सिरे से मनुष्य को प्राप्त नहीं रहता अपितु उसको निश्चित करना ईश्वर का स्वत्व हो जाता है। इसके बाद नीति शास्त्र के वे समस्त प्रश्न जिनको तत्व विचारकों ने छेड़ा है न केवल यह कि हल हो जाते हैं वरन् इस बात का भी अवकाश शेष नहीं रहता कि एक-एक प्रश्न के छत्तीस उत्तर हों और एक-एक उत्तर पर मनुष्य का एक-एक समूह नीति की एक पृथक दिशा में चल पड़े और एक ही सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में रहते हुए यह विभिन्न दिशाओं में चलने वाले लोग अपनी कुचाल से अव्यवस्था, विशृंखलता एवं उपद्रव मचायें। यदि मनुष्य की इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाय जो इस्लाम ने निश्चित की है तो यह बात स्वयं निश्चित हो जाती है कि ईश्वर की परीक्षा में सफल होना और उसकी इच्छा की पूर्ति करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेना ही वह सर्वोत्तम भलाई है जो स्वमेव लक्ष्य होना चाहिए और किसी व्यवहार नीति के शुद्ध अशुद्ध होने का आश्रय इसी पर है कि वह उस भलाई की प्राप्ति में कहाँ तक सहायक अथवा बाधक होती है। इसी प्रकार यह बात भी यहीं से निश्चित हो जाती है कि मनुष्य के लिए बुरे और भले शुद्ध और अशुद्ध के ज्ञान का वास्तविक मूलाधार ईश्वरीय मार्ग-दर्शन है और इसके सिवा दूसरे ज्ञान स्रोत इस वास्तविक मूलाधार के सहायक तो बन सकते हैं परन्तु स्वयं यथार्थ मूलाधार नहीं बन सकते, और यह कि नैतिक नियम के लिए वास्तविक नैतिक आदेश (Sanction) ईश्वर का है और यह भी कि श्रेष्ठ नैतिक नियमों का पालन और दुराचार से विरक्ति का वास्तविक प्रेरक ईश्वर का प्रेम उसकी प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा और उसकी अप्रसन्नता तथा कोप का भय होना चाहिए, फिर न केवल यह कि इससे नीति शास्त्र के समस्त सैद्धांतिक प्रश्न हल हो जाते हैं अपितु इस आधार पर, वस्तुतः जो नैतिक व्यवस्था बनती है उसके भीतर अति संतुलित एवं संगठित रूप से समस्त नैतिक सिस्टम अपना-अपना उचित स्थान पा लेते हैं जो नैतिक शास्त्र के विचारकों ने प्रस्तुत किये हैं। दार्शनिक नीति-व्यवस्थाओं की वास्तविक त्रुटि यह नहीं है कि इनमें वास्तविकता एवं सत्यता का कोई अंश भी नहीं है अपितु उनका मूल दोष यह है कि उन्होंने सत्य के एक अंश को लेकर पूर्ण-सत्य बना लिया है। अतः अंश को पूर्ण बनाने में जिस मात्रा में पूरक की आवश्यकता होती है इसके लिए उन्हें निस्सन्देह असत्य के बहुत से अंश लेने पड़ते हैं। इस्लाम इसके विपरीत पूर्ण सत्य प्रस्तुत करता है और इस पूर्ण सत्य में वे समस्त आंशिक सत्य सम्मिलित हो जाते हैं जो लोगों के पास अलग-अलग थे और अपूर्ण थे। यहाँ आनन्द का भी एक स्थान है किन्तु इससे तात्पर्य वह आनन्द अथवा कल्याण है जो ईश्वरीय विधि के अनुवर्तन से और उसके फलस्वरूप प्राप्त हो और यह आनन्द दैहिक एवं भैतिक भी है, मानसिक एवं आत्मिक भी, और आटिस्टिक एवं आध्यात्मिक भी। तथा यह आनन्द एवं कल्याण व्यक्ति का भी है समाज का भी और समस्त मानव-जाति का भी। इन विभिन्न आनन्दों में संघर्ष नहीं सहयोग है। यहां निपुणता तथा उत्कर्ष का भी एक स्थान है किन्तु वह उत्कर्ष जो ईश्वर की परीक्षा में सौ प्रतिशत नम्बर पाने का पात्र हो और यह व्यक्ति का, जनसमूह का, जाति का सम्पूर्ण मानव मात्र का, आशय यह कि सब ही का उत्कर्ष है। उचित नैतिक व्यवहार वह है जिससे प्रत्येक व्यक्ति न केवल स्वयं उत्कर्ष की ओर उन्नति करे और शिरोबिन्दु तक पहुंचने की चेष्टा करे अपितु अन्य व्यक्तियों के प्रयास में भी सहायक हो और कोई किसी के प्रयास में बाधक न हो। यहाँ कान्ट के निरपेक्ष विधि (Categorical Imperative) को भी उचित स्थान प्राप्त हो जाता है और इस जहाज़ को वह लंगर भी मिल जाता है जिसके बिना वह दर्शन शास्त्र के समुद्र में डगमगा रहा था। जिस निरपेक्ष विधि का उल्लेख कान्ट ने किया है और जिसकी वह स्वयं कोई व्याख्या न कर सका, वास्तव में वह ईश्वर की विधि है, ईश्वर ही की ओर से उसका रूप नियत हुआ है और ईश्वर ही की विधि होने के कारण उसका अनुवर्तन अनिवार्य है और ननुनच के बिना उसी के आज्ञापालन का नाम पुण्य है। इसी प्रकार यहाँ नैतिक पाप पुण्य के ज्ञान का जो मूलाधार हमें बताया गया है वह इन दूसरे ज्ञान साधनों का निषेध नहीं करता जिनसे तत्व विचारक काम लेते हैं अपितु इन सबको एक सिस्टम का अंश बना लेता है। हाँ वह निषेध जिस वस्तु का करता है वह केवल यह बात है कि उन्हें या उसमें से किसी एक को यथार्थ एवं अन्तिम ज्ञान साधन के रूप से ले लिया जाए। ईश्वरीय आदेश के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्रदान किया गया है वह यथार्थ ज्ञान है और प्रयोग-साध्य ज्ञान, प्राकृतिक नियम और अस्तित्व की अवस्थाओं से विवेचन करके प्राप्त किया हुआ ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान और भावनात्मक ज्ञान, यह सब इसके साक्ष्य हैं। जिन वस्तुओं को ईश्वर का आदेश पुण्य कहता है, मानवता का अनुभव उसके पुण्य होने पर गवाही देता है, प्राकृतिक नियम उसका समर्थन करते हैं, बुद्धि और भाव रस दोनों इस पर साक्ष्य हैं। किन्तु सत्यता का मापदण्ड ईश्वरीय आदेश है न कि यह ज्ञान साधन। मानवता के ऐतिहासिक अनुभव से या प्राकृतिक नियमों से यदि विवेचन करके कोई ऐसा फल प्राप्त किया जाय जो ईश्वरीय आदेश के विरुद्ध हो तो वास्तविक विश्वास ईश्वर के आदेश का किया जायेगा न कि इस विवेचन या उस मत का। हमारे पास ज्ञान का एक पारिमाणिक मापदण्ड होने का लाभ ही यह है कि हमारे ज्ञान में डिसिप्लिन उत्पन्न हो और हम उस विशृंखलता तथा अव्यवस्था से बच जायें जो किसी माप-दण्ड के अभाव और "प्रत्येक राय रखने वाले के अपनी ही राय पर गर्व" से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यहां नैतिक नियम की पृष्ठि पर काम करने वाली शक्ति, नैतिक आदेश (Sanction) तथा प्रेरकों की समस्या भी इस प्रकार हल हो जाती है कि इससे उन अन्य वस्तुओं का निषेध नहीं होता जो तत्वविचारकों ने प्रस्तुत किये हैं अपितु केवल उनका संशोधन हो जाता है और जिन अशुद्ध सीमाओं पर वह फैला दी गई हैं या स्वयं फैल जाती हैं वहां से उनको हटाकर एक संगठित एवं सर्वव्यापी व्यवस्था में ठीक स्थान पर रख दिया जाता है। ईश्वर की विधि इसलिए कि वह ईश्वर की विधि है, अपनी स्थापना की शक्ति आप अपने भीतर रखती है और यह शक्ति उस मोमिन (आस्तिक) के व्यक्तित्व में भी उपस्थित है जो ईश्वर की प्रसन्नता चाहने में आनन्द अनुभव करता है और स्वयं उस उत्कर्ष का इच्छुक है जो ईश्वर की ओर बढ़ने से प्राप्त हो तथा यह शक्ति मोमिनों (आस्तिकों) की सोसाइटी और उस पवित्र स्टेट में भी विद्यमान है जो ईश्वर के विधान पर आश्रित हो। विधान के पालन पर मोमिन को उत्सुक करने वाली वस्तु उसकी विशुद्ध कर्त्तव्य-परायणता भी है, इसका सत्य को सत्य जानते हुये पसंद करना और असत्य को असत्य समझते हुए उससे घृणा करना भी है और वह लालसा और भय भी है जो वह अपने ईश्वर से रखता है।
देखिये, इस प्रकार इस्लाम उस पूर्ण विचारात्मक एवं व्यावहारिक विश्रृंखलता (anarchy) का उन्मूलन कर देता है जो मनुष्य को निरीश्वर कल्पना करके उसके लिये एक नीति-व्यवस्था प्रतिपादित करने के प्रयास से उत्पन्न होती है। इसके बाद आगे चलिये। इस्लाम ईश्वर की जो कल्पना प्रस्तुत करता है वह यह है कि ईश्वर ही मनुष्य का और अखिल विश्व का एक मात्र स्वामी सृजनहार, विधाता, विश्वंभर, पूज्य तथा अधिशासक है। इस ईश्वरत्व में कोई उसका सहभागी नहीं है। इसके यहां कल्याण हेतु सविनय निवेदन के अतिरिक्त किसी ऐसी अनुशंसा का अवकाश भी नहीं जो बलपूर्वक मनवाई जाती हो और रद्द न की जा सकती हो। इसके यहाँ प्रत्येक की सफलता एवं विफलता का आधार उसके अपने आचार व्यवहार पर है न कोई किसी के लिये प्रायश्चित कर सकता, न किसी के आचार व्यवहार का दायित्व दूसरे पर डाला जाता है और न दूसरे के कर्मों का फल दूसरा भोगता है। उसके यहाँ पक्षपात नहीं कि एक व्यक्ति वंश, कुटुम्ब अथवा जाति की ओर उसको दूसरी की अपेक्षा अधिक रुचि हो। सारे मनुष्य उसकी दृष्टि में समान हैं, सबके लिये एक ही नैतिक नियम है और श्रेष्ठता जो कुछ भी है नैतिक उत्कर्ष के आधार पर है। वह स्वयं दयालु एवं कृपालु है और क्षमाशीलता को पसंद करता है। वह स्वयं उदार है और उदारता को पसंद करता है। वह स्वयं न्यायिक है और न्याय को पसन्द करता है। वह स्वयं अत्याचार, दृष्टि-संकीर्णता, पाषाणहृदयता, कृपणता क्रूरता, स्वार्थ-प्रियता एवं पक्षपात से रहित है, अत: उन्हीं को पसंद करता है जो इन अवगुणों से रहित हों। फिर प्रभुता एकमात्र उसी का स्वत्व है अत: दंभ उसे अरुचिकर है। ईश्वरत्व केवल उसके लिये है और दूसरे उसके दास हैं इसलिये एक दास पर दूसरे का प्रभुत्व उसको रुचिकर नहीं। स्वामी वह अकेला है और दूसरों के पास जो कुछ है थाती के रूप में है अतएव किसी दास की स्वाधीनता और किसी का किसी के लिये विधान निर्मित करना और किसी का किसी के लिये स्वतएव आज्ञापक अथवा आज्ञापालन के योग्य होना ये सब वस्तुत: अशुद्ध हैं। सबका आज्ञापक वही है और सबका कल्याण इसी में है कि उसका आज्ञापालन ननुनच के बिना करें। फिर वह उपकारक है और कृतज्ञता-प्रकाशन धन्यवाद तथा प्रेम का पात्र है। वह प्रदाता है और इसका स्वत्वधारी है कि उसकी प्रदत्त निधियों को उसके अनुसार प्रयोग में लाया जाय। वह न्यायिक है और यह अनिवार्य है कि मनुष्य उसके न्याय में दण्ड भोगने का भय और प्रतिफल पाने की लालसा रखे। वह सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शक है और हृदय एवं चित्त-वृत में छिपे हुये संकल्पों से भी अवगत है इसलिये बाह्य शिष्ट स्वभाव तथा दिखावटी सदाचार से उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। वह सर्वव्यापक है, इसलिये कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि अपराध करके उसकी पकड़ से बच निकलेगा।
ईश्वर की इस कल्पना पर विचार कीजिये, इससे स्वत: एक प्राकृतिक फल के रूप में मनुष्य के लिये एक सम्पूर्ण नैतिक जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत होती है और वह रूपरेखा उन समस्त त्रुटियों से रिक्त है जो बहुदेववादी मतों एवं निरीश्वरवादी पंथों के नीतिशास्त्रों में पाई जाती है। यहाँ न तो नैतिक दायित्वों से बच निकलने के लिये चोर दरवाज़े कहीं विद्यमान हैं, न उन अन्यायपूर्ण तत्वों के लिये कोई स्थान है जिनके आधार पर मनुष्य अपनी रुचियों के अनुसार मानव-जाति को विभाजित करके एक भाग के लिये देवता और दूसरे भाग के लिए दानव बन जाता है। न निरीश्वरवादी नीतिशास्त्र की वह मौलिक त्रुटियाँ इसमें पाई जाती हैं जिनके कारण नैतिकता में कोई स्थायित्व उत्पन्न नहीं हो सकता। इन निषेधात्मक (Negative) गुणों के साथ इस रूपरेखा में यह विधानात्मक (Positive) गुण विद्यमान है कि यह नैतिक उत्कर्ष की एक उच्चतम एवं विशालतम चरम सीमा प्रस्तुत करता है जिसकी उच्चता एवं विशालता की कोई सीमा नहीं और उस पराकाष्ठा की ओर बढ़ने के लिये ऐसे प्रेरक एकत्र करता है जो पवित्रतम हैं।
फिर यह कल्पना कि परीक्षा किसी एक वस्तु में नहीं है वरन् उन समस्त वस्तुओं में है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की हैं, किसी एक स्थिति में नहीं अपितु उन समस्त स्थितियों में है जो मनुष्य को यहाँ प्राप्त है और किसी एक विभाग में नहीं वरन् पूर्ण जीवन में है। यह नैतिकता के वृत को उतना ही फैला देता है जितना परीक्षा-स्थल फैला हुआ है। मनुष्य की बुद्धि उसके ज्ञान-साधन उसकी मानसिक एवं चिन्तन शक्तियाँ, उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ, उसके मनोवेग, उसकी इच्छायें, उसकी शारीरिक शक्तियाँ, सबकी सब परीक्षा में सम्मिलित हैं अर्थात् परीक्षा मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व की है। फिर बाह्य संसार की जिन-जिन वस्तुओं से मनुष्य का सम्पर्क होता है, जिन वस्तुओं पर वह अधिकार रखता है, जिन मनुष्यों से विभिन्न स्थितियों में उसका सम्बन्ध होता है उन सबके प्रति उसके व्यवहार में परीक्षा है, और सबसे बढ़कर इस बात में परीक्षा है कि मनुष्य यह सब कुछ ईश्वर के ईश्वरत्व तथा अपने दासत्व की अनुभूति के साथ कर रहा है या स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के भाव में लीन होकर या ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य का दास बनकर। इस अति विस्तीर्ण नैतिक कल्पना में वह संकीर्णता नहीं है जो धर्म की सीमित कल्पना से उत्पन्न होती है। यह मनुष्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाती है, प्रत्येक क्षेत्र के नैतिक दायित्व उसे बताती है और वह नैतिक सिद्धान्त उसे देती है जिनके अनुवर्तन से वह ईश्वर की उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके जो जीवन के एक-एक क्षेत्र से समबद्ध है।
फिर यह कल्पना कि परीक्षा का वास्तविक तथा अन्तिम निर्णय इस जीवन में नहीं अपितु मरणोत्तर जीवन में होगा और वास्तविक सफलता एवं विफलता वह है जो वहाँ हो न कि यहाँ, यह संसार का जीवन तथा उसके विषयों पर मनुष्य के दृष्टिकोण को मूलत: परिवर्तित कर देता है। इस कल्पना के कारण वह फल जो इस संसार में निकलते हैं हमारे लिये गुण अवगुण, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, तथा सफलता एवं विफलता के निरपेक्ष यथार्थ तथा अन्तिम मापदण्ड नहीं रहते अत: नैतिक नियमों के अनुवर्तन अथवा अतिक्रमण का अवलंबन भी उन फलों पर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस कल्पना को स्वीकार करेगा वह नैतिक नियमों का अनुवर्तन प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता पूर्वक करेगा, चाहे इस संसार में उसका परिणाम प्रत्यक्षत: अच्छा हो या बुरा, सफलता के रूप में निकलता दिखाई दे अथवा विफलता के रूप में। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसकी दृष्टि में लौकिक परिणाम सर्वथा उपेक्ष्य होंगे अपितु उनका अर्थ केवल यह है कि वह वास्तविक एवं अन्तिम महत्त्व इनको नहीं वरन् मरणोत्तर जीवन के दृढ़ स्थायी परिणामों को देगा और अपने लिये केवल उस व्यवहार-नीति को उचित समझेगा जो इन परिणामों पर दृष्टि रखते हुये ग्रहण की जाय। वह किसी वस्तु को त्याज्य और किसी को ग्राह्य इस आधार पर नहीं समझेगा कि जीवन की इस प्रारम्भिक श्रेणी में वह स्वादिष्ट आनन्द दायक तथा लाभप्रद है अथवा नहीं, अपितु इस आधार पर समझेगा कि जीवन की अन्तिम श्रेणी पर अपने निरपेक्ष एवं स्थायी परिणामों की दृष्टि से वह कैसी है। इस प्रकार उसकी नैतिक व्यवस्था उन्नतिशील तो अवश्य रहेगी किन्तु उसके नैतिक सिद्धान्त परिवर्तन-शील न होंगे और न इसका आचरण ही अस्थिरचित होगा अर्थात् सभ्यता एवं संस्कृति की वृद्धि एवं विकास के साथ-साथ इसकी नैतिक कल्पनाओं में विस्तार तो अवश्य होगा। किन्तु यह सम्भव न होगा कि घटनाओं की प्रत्येक करवट और परिस्थितियों के प्रत्येक चक्र के साथ नीति के सिद्धान्त भी परिवर्तित होते चले जायें और मनुष्य एक नैतिक गिरगिट बनकर रह जाय, कि उसकी नैतिक मनोवृत्ति में सिरे से कोई स्थायित्व ही न हो। अत: नैतिक दृष्टिकोण से मरणोत्तर जीवन की यह इस्लामी कल्पना दो महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है जो किसी अन्य साधन से उपलब्ध नहीं हो सकते। एक यह कि इससे नैतिक सिद्धान्तों को दृढ़तम आधार प्राप्त होता है जिसमें अस्थिरता का कोई भय नहीं। दूसरे यह कि इससे मनुष्य के नैतिक आचरण को वह स्थायित्व प्राप्त होता है जिसमें (यदि धर्मनिष्ठा है तो) विचलन की कोई आशंका नहीं। संसार में सच्चाई के दस विभिन्न परिणाम निकल सकते हैं और उन परिणामों पर दृष्टि रखने वाला एक अवसरवादी मनुष्य अवसर एवं सम्भावनाओं की दृष्टि से दस विभिन्न व्यवहार-रीतियाँ ग्रहण कर सकता है किन्तु परलोक में सच्चाई का परिणाम अनिवार्यत: एक ही है और उस पर दृष्टि रखने वाला एक आस्तिक व्यक्ति ऐहिक लाभ हानि की चिन्ता किये बिना अनिवार्यत: एक ही व्यवहार-रीति ग्रहण करेगा। सांसारिक परिणामों का विश्वास कीजिये तो पाप पुण्य किसी निश्चित वस्तु का नाम नहीं रहता वरन् एक ही वस्तु अपने विभिन्न विचार से कभी पुण्य कभी पाप बनती रहती है, और इसके अनुवर्तन में संसार-पूजक मनुष्य का आचरण भी अपना अधिष्ठान बदलता रहता है, किन्तु परलोक के परिणामों पर दृष्टि रखिये तो पाप पुण्य दोनों सर्वथा निश्चित हो जाते हैं और आस्तिक जो मरणोत्तर जीवन पर विश्वास रखता है उसके लिये यह असम्भव हो जाता है कि कभी पुण्य को हानिकारक और पाप को लाभप्रद समझकर अपना आचरण बदल दे।
फिर यह कल्पना कि मनुष्य इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे जो अधिकार यहां प्राप्त हैं वे सब वास्तव में ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते हैं, मानव-जीवन के लिए उद्देश्य एवं मार्ग दोनों निश्चित कर देती है। इस कल्पना से अनिवार्य हो जाता है कि मनुष्य के लिये स्वाधीनता, ऐश्वर्य तथा अन्य की भक्ति आदि की समस्त कार्यशैलियां अशुद्ध हों केवल यही एक मनोवृत्ति शुद्ध हो कि अपने अधिकारों में वह ईश्वर की इच्छा का आधीन और उसके उतारे हुये नैतिक आदेशों का आबद्ध बनकर रहे, तथा इससे यह भी अनिवार्य हो जाता है कि मनुष्य एक ओर तो अपनी नैतिक युक्ति में प्रत्येक ऐसी व्यवहार-रीति से पूर्णरूपेण विरक्त रहे जिसमें स्वाधीनता एवं ईश द्रोह का, या ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की भक्ति का, अथवा ऐश्वर्य का लेशमात्र अंश पाया जाता हो। क्योंकि यह तीनों वस्तुएं उसके प्रतिनिधित्व-पद के विरुद्ध हैं, किन्तु दूसरी ओर ईश्वर के स्वामित्व में उसका अधिकार और ईश्वर की उत्पन्न की हुई शक्तियों में उसका व्यवहार और ईश्वर की प्रजा पर उसका शासन उस नीति तथा उस व्यवहार के सर्वथा अनुकूल हो जो इस राज्य का यथार्थ अधिशासक, अपने राज्य और अपनी प्रजा के सम्बन्ध में ग्रहण कर रहा है, क्योंकि प्रतिनिधित्व के पद की स्वाभाविक अपेक्षा यही है कि प्रतिनिधि की पॉलीसी स्वयं अधिशासक की पॉलीसी के और उपाध्यक्ष की नीति स्वयं अध्यक्ष की नीति के विरुद्ध न हो, तथा इस कल्पना से यह भी अनिवार्य हो जाता है कि जो शक्तियाँ ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की हैं और जो साधन एवं उपकरण उसे संसार में दिये गये हैं उन सबको प्रयोग करने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रयोग करने पर मनुष्य नियुक्त हो, अर्थात् अन्य शब्दों में वह उपाध्यक्ष भी घोर अपराधी तथा नीतिभ्रष्ट हो जिसने अध्यक्ष की इच्छा के प्रतिकूल उसकी मिल्कियत अथवा प्रजा में हस्तक्षेप किया और इसी प्रकार वह उपाध्यक्ष भी बड़ा अपराधी समझा जाय जिसने अध्यक्ष के दिये हुये अधिकारों में से किसी अधिकार को सिरे से प्रयोग ही न किया हो, उसकी प्रदान की हुई शक्तियों में से किसी शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट किया हो, उसके बनाये हुए साधन तथा उपकरण से काम लेने में जान-बूझकर कोताही की हो और इस ड्यूटी से मुँह मोड़ कर खड़ा हो गया हो जिस पर अध्यक्ष ने उसे नियुक्त किया था। तथा इस कल्पना से यह भी अनिवार्य हो जाता है कि पूरी मानव जाति का सामाजिक जीवन ऐसे ढंग पर स्थापित हो कि सारे मनुष्य अर्थात ईश्वर के सब उपाध्यक्ष उन उत्तरदायित्वों का पालन करने में जो ईश्वर ने उन पर डाल दिये हैं, एक दूसरे के सहायक तथा सहयोगी हों और सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में ऐसी कोई वस्तु चलने न पाये जिसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की, या मनुष्यों का एक वर्ग दूसरे वर्ग की उपाध्यक्षता को व्यवहारत: छीन ले या उसके चरितार्थ होने में बाधक हो, सिवाय उस अवस्था के जबकि कोई मनुष्य अथवा समुदाय मानुषिक उपाध्यक्षता से विमुख होकर अपने वास्तविक अध्यक्ष से विद्रोह कर रहा हो।
यह तो है वह नैतिक मार्ग जो उपाध्यक्षता की कल्पना से एक अनिवार्य फल के रूप में मनुष्य के लिये बनता है। रहा मनुष्य के नैतिक जीवन का उद्देश्य और उसके समस्त प्रयास तथा आचार व्यवहार का आदर्श तो वह भी इस कल्पना से सर्वथा एक तार्किक उपसंहार के रूप में निश्चित होता है। उपाध्यक्ष की स्थिति में मनुष्य की पृथ्वी पर नियुक्ति स्वयं इस बात का अधियाचक है कि मनुष्य के नैतिक जीवन का उद्देश्य पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ न हो। ईश्वर ने पृथ्वी के प्रबन्ध का जितना भाग मनुष्य से सम्बद्ध किया है उस भाग में ईश्वर के विधान को जारी करना, ईश्वर की इच्छा के अनुसार शांति, न्याय एवं सुधार की व्यवस्था स्थापित करना तथा स्थिर रखना, इस व्यवस्था में उपद्रव एवं विद्रोह के जितने रूप 'जिन्न' अथवा 'मानव' रूपी दानव उत्पन्न कर उनको दबाना, मिटाना और उन भलाइयों को अधिकाधिक बढ़ना एवं विकसित करना जो ईश्वर को प्रिय हैं जिनसे विश्वंभर अपनी पृथ्वी तथा अपनी प्रजा को सुसज्जित देखना चाहता है। यह है वह उद्देश्य जिस पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्त चेष्टाओं को केन्द्रित कर देगा जिसके भीतर ईश्वर के उपाध्यक्ष होने की चेतना जाग्रित हो चुकी हो। यह उद्देश्य केवल यही नहीं कि उन समस्त उद्देश्यों को निषेध कर देता है जो भौतिक वादियों स्थूलवादियों, स्वादपूजकों, जातिभक्तों तथा अन्य निरर्थक वस्तुओं के पूजकों ने अपने जीवन के लिये निश्चित किये हैं अपितु उन व्यर्थ उद्देश्यों का भी उतनी ही उग्रता से निषेध करता है जो आध्यात्मिकता की एक भ्रममूलक तथा अशुद्ध कल्पना के अन्तर्गत धार्मिक वर्ग ने नियत किये हैं। इन दोनों अशुद्ध चरम सीमाओं के बीच ईश्वर की उपाध्यक्षता की कल्पना मनुष्य के सम्मुख एक ऐसा उच्चतम एवं पवित्रम जीवन ध्येय रख देती है जो उसकी समस्त शक्तियों एवं योग्यताओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें एक पवित्रतम सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना एवं विकास हेतु प्रयुक्त करता है।
यह हैं वे आधार जो मानव-नैतिकता के निर्माण हेतु इस्लाम ने हमको दिये हैं। इस्लाम किसी जाति विशेष की सम्पत्ति नहीं अपितु समस्त मानवजाति की संयुक्त सम्पत्ति है और सारे मनुष्यों का कल्याण उसकी दृष्टि में है अत: प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपना और मानवता के कल्याण का इच्छुक हो यह सोचना चाहिये कि क्या मानव-नीति के निर्माण हेतु यह आधार श्रेष्ठतम है जो इस्लाम हमें दे रहा है या वह जो आध्यात्मिक मत अथवा दार्शनिक पन्थ हमको देते हैं? यदि किसी का दिल गवाही दे कि नैतिकता के लिए यही आधार श्रेष्ठतम हैं तो फिर कोई अज्ञानपूर्ण पक्षपात उसे इन आधारों के स्वीकार कर लेने में बाधक न होना चाहिये।
(E-Mail: HindiIslamMail@gmail.com Facebook: Hindi Islam, Twitter: HindiIslam1, YouTube: HindiIslamTv )
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
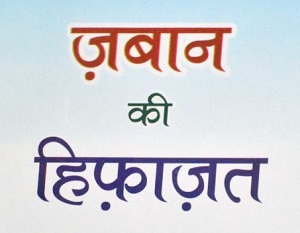
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
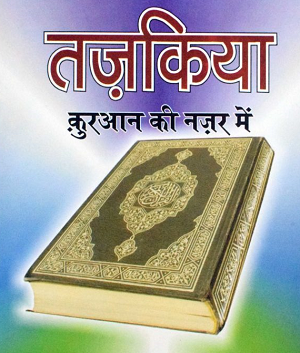
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

