
इस्लाम में बलात् धर्म परिवर्तन नहीं
-
इस्लाम
- at 30 March 2020
इमामुद्दीन रामनगरी
इस्लाम को लेकर आम लोगों में बहुत ग़लतफ़हमियां फैली हुई है। इसका बुनियादी कारण यह है कि इस्लाम के अनुयायियों ने उन लेगों के बीच इस्लाम का परिचय नहीं कराया, जो इस्लाम से अपरिचित थे, जबकि आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि उन लोगों तक इस्लाम के पैग़ाम को पहुंचाएं, जिन तक यह नहीं पहुंचा है। इस के अलावा कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए इस्लाम के विरुद्ध जो द्वेषपूर्ण तथा निराधार प्रचार कर के इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश भी की है और इस्लाम के बिरुद्ध कई तरह की भ्रांतियों को हवा दी है। यह पुस्तिका ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश है। विशेष रूप से इस में जिहाद और जिज़्या की वास्तविकता पर बात की गई है। यह पुस्तिका पहली बार 1945 ई० में प्रकाशित हुई थी। आज भी इसकी प्रसांगिकता कम नहीं हुई है। -संपादक
“अल्लाह, अत्यन्त दयावान, कृपाशील के नाम से”
जिहाद और जिज़्या की वास्तविकता
हर प्रकार की स्तुति, प्रशंसा कृतज्ञता अल्लाह के लिए है और अल्लाह की अनन्त दया व कृपा हो उसके सभी रसूलों पर।
इस्लाम की शुरूआत मक्का में हुई। मक्का निवासी बिलकुल धर्मभ्रष्ट तथा आचारहीन थे। उन्होंने 13 वर्ष तक मक्का में इस्लाम का विरोध किया तथा पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और मुसलमानों के देश त्यागकर मदीना चले जाने के बाद भी युद्ध द्वारा इस्लाम और मुसलमानों का उन्मूलन करने का प्रयत्न करते रहे। मदीना के आप-पास यहूदियों की बस्तियों थीं। वे भी इस्लाम के विरोधी बन गए। आगे चलकर ईरान और रोम के साम्राज्य इस्लाम के शत्रु, बनकर उठ खड़े हुए। यूरोप में इस्लाम पहुँचा तो ईसाइयों ने इस्लाम के विरुद्ध दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने यहाँ भी वही ग़लतफ़हमी फैलाई। भारत के निवासियों में स्वामी दयानन्द जैसे धार्मिकों और यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने इस्लाम विरोधी भ्रष्ट साहित्य का प्रचार किया। इस्लाम विरोधियों ने जिन विषयों को लेकर दुष्प्रचार किया, उनमें दो विषय बहुत आम है, एक ‘जिहाद' और दूसरा ‘जिज़्या'। कहा जाता है कि इस्लाम गै़र मुस्लिमों को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का आदेश देता है तथा बल ही के द्वारा इस्लाम फैला और जिज़्या का उद्देश्य भी यह है कि ग़ैर-मुस्लिमों को कर भार द्वारा इस्लाम ग्रहण करने पर मजबूर किया जाए।
बलात् धर्म परिवर्तन और इस्लाम
संसार के जिन सम्प्रदायों से इस्लाम को सबसे पहले वास्ता पड़ा वे यहूदी और ईसाई सम्प्रदाय थे। यहूदियों की इस्लाम के केन्द्र मदीना के आस-पास बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थीं और उनका अरबों पर बड़ा प्रभाव था और ईसाईयों के विशाल साम्राज्य का क्षेत्र मदीना निवासियों की सीमा तक फैला हुआ था और उसके प्रभाव से लाखों अरब ईसाई हो गए थे। सीमा प्रान्त में कुछ अरब रियासतें भी स्थापित हो गई थीं । यमन का नजरान प्रान्त ईसाइयों का केन्द्र था।
यहूदी और ईसाई अगर अपने-अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन करते होते और अपने-अपने धर्मग्रन्थों के अनुसार चलते होते तो दोनों को मुसलमान होना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम के सिद्धान्त और इतिहास के अनुसार संसार के विभिन्न देशों और जातियों में जितने भी नबी, रसूल और ईशदूत हुए थे, उन सबने इस्लाम ही की शिक्षा दी थी और इसी की ओर लोगों का मार्गदर्शन किया था और उन्हीं में हज़रत मूसा और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) भी थे, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों में से कोई सम्प्रदाय भी अपने रसूलों की दी हुई शिक्षा पर क़ायम न था। यहूदी ‘तौरात' से बिमुख हो गए थे और ईसाई इंजील से। इतना ही नहीं, दोनों ने इन ग्रन्थों में हेर-फेर भी कर दिया था और इनको अपनी इच्छा और स्वार्थ के अनुसार बना लिया था।
क़ुरआन ने इस्लाम के सिद्धान्त के अनुसार तौरात और इंजील दोनों को ईश्वरीय ग्रन्थ माना और हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) दोनों को (उन पर ईश्वर की दया और कृपा हो) ईश्वर का सच्चा सन्देशदाता स्वीकार किया और इसी के साथ यहूदियों और ईसाइयों के आलिमों ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए तौरात और इंजील में जो कांट-छांट कर दी थी, उसको भी प्रकट कर दिया और इस प्रकार यहूदियों और ईसाइयों के विद्धानों का पोल खुल गया। उनकी महात्माई धूल में मिल गई तथा उनका खाने-कमाने और भोग-विलास का अधिकार ख़त्म हो गया । इस कारण अनिवार्य था कि यहूदी और ईसाई सम्प्रदाय इस्लाम के शत्रु बन जाएँ।
यहूदियों और ईसाइयों के विद्वानों और धर्मगुरूओं ने ईश्वर के लिए नियम और क़ानून, हराम और हलाल को उठाकर अलग रख दिया था और ईश्वर के नाम से अपने नियम और अपनी आज्ञा चला रहे थे। क़ुरआन ने उन दोनों के भ्रष्टाचार के बारे में कहा-
‘‘यहूदियों के पंडितों और ईसाईयों के सन्तों में बहुत से ऐसे हैं जो लोगों के धन को अवैध रूप से खाते हैं और उनको ख़ुदा के रास्ते पर चलने से रोकते हैं।'' (क़ुरआन-9:34)
यहूदी आज की तरह उस काल में भी बड़े पूंजीपति थे और सूद-ब्याज, छल-कपट और अत्याचार हर प्रकार से धन प्राप्त कर लेने के लिए लालायित रहते थे, हालाँकि उनके धर्म में सूद लेना मना था। क़ुरआन में कहा गया है-
‘‘यहूदियों के सूद लेने पर हालाँकि उनको इससे मना कर दिया गया था और उनके भ्रष्ट रीति से धन खाने पर (उनको यह दण्ड दिया गया कि पवित्र चीजें भी जो उनपर हलाल थीं हराम ठहरा दी गईं)।'' (क़ुरआन-4:161)
तौरात और इंजील में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का पूरा परिचय दिया हुआ था और उन धर्मग्रन्थों के पण्डित और विद्वान इस परिचय से भली-भाँति अवगत थे। उनको आशा थी कि आप उन्हीं की जाति में पैदा होंगे। इसीलिए वे आपके आने की प्रतिक्षा भी कर रहे थे, लेकिन आप का जन्म दूसरे वंश में हुआ तो यहूदी और ईसाई दोनों आपके विरोधी बन गए। इस सम्बन्ध में एक जगह क़ुरआन में कहा गया है-
‘‘हमने जिन लोगों को ग्रन्थ दिया था वे (अपने ग्रन्थ द्वारा) उनको उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह वे अपनी सन्तान को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक समुदाय जान-बूझकर सत्य को छिपा रहा है।'' (क़ुरआन-2:146)
उन्हीं में जो सत्यप्रिय थे उन्होंने हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को और क़ुरआन शरीफ़ को मान लिया। उनके सम्बन्ध में क़ुरआन में कहा गया है-
‘‘(इनमें ऐसे भी है कि) जब वे उन बातों को सुनतें हैं जो रसूल (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उतारी गई हैं, तो तू उनकी आँखों को देखता है कि उनसे आँसू बहने लगते हैं, इस वजह से कि वे सत्य से परिचित हो गए।'' (क़ुरआन-5:83)
यहूदी इस्लाम को हानि पहुँचाने के लिए तरह-तरह के छल-कपट से काम लेते। क़ुरआन में है-
‘‘किताबवालों में एक समुदाय ऐसा है जो आपस में कहता है कि मुसलमानों पर जो ग्रन्थ उतारा गया है, उसपर दिन के आरम्भ में ईमान लाओ और दिन के अन्त में उससे नकार कर दो, शायद (इस तरकीब से) मुसलमान भी इस्लाम से पलट जाएँ।'' (क़ुरआन-3:72)
यहूदी पूँजीपति अवश्य थे, फिर भी उनके पास न कोई बड़ा राज्य था और न सैनिक शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी कूटनीति से मदीना में प्रभाव जमा रखा था। हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ख़ुदा के बहुत बड़े पैग़म्बर और इस्लाम के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मक्का में एकेश्वरवाद का केन्द्र (काबा) स्थापित किया था। लेकिन उनकी सन्तान धीरे-धीरे उनकी शिक्षा को भुला बैठी थी और उनके पथ से भटककर बहुत-से देवताओं के चक्कर में पड़ गई थी। वे लोग अपनी इस पथभ्रष्टता के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पतन के गढे़ में जा गिरे थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की संतान के उस गोत्र में पैदा हुए जो काबा का पुरोहित और प्रबन्धक था। लेकिन आप अपने दादा के धर्म के उपदेशक और एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। इसी लिए आपके गोत्र ही के लोग आपके सबसे बड़े विरोधी और देश भर के विरोधियों के नेता बन गए थे और उनको सैन्य शक्ति से कुचल डालना चाहते थे और मदीना के यहूदी इन लोगों से सदा छिपे-खुले सम्बन्ध रखते थे। इनकी जासूसी करते थे और हर प्रकार की सहायता देते थे, परन्तु इस्लाम अपने बौद्धिक विश्वासों, प्राकृतिक सिद्धान्तों, दिव्य शिक्षा, उन्नत पथ और नैतिक आदर्श के बल पर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया। यहूदियों का ज़ोर टूट गया, अरब पराजित हो गए, देश भर में इस्लाम का कोई प्रतिद्वन्द्वी बाक़ी नहीं रह गया। अरब की सीमा पर ईसाइयों का रोमन आधिपत्य था, उसने इस्लाम से टक्कर ली, उसे भी हार माननी पड़ी। शाम (सीरिया) से रोमन साम्राज्य का झण्डा उखड़ गया और फ़िलस्तीन जो यहूदियों और ईसाईयों का धर्म केन्द्र था और जिस पर हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) और हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के सच्चे प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी के नाते मुसलमानों का हक़ था वह भी मुसलमानों के अधिकार में आ गया। इसी प्रकार मुसलमान सत्य-धर्म की पताका लिए हुए यूरोप में पहुँच गए।
झूठ के प्रचार में यूरोप कितना आगे है यह कोई ढंकी-छिपी बात नहीं है, वह इस कला का पुराना माहिर है। ईसाई बादशाहों की तलवारें मुसलमानों का मुक़ाबला कर रही थीं और ईसाई, पोपों , पादरियों और विद्वानों की ज़बानें और क़लम इस्लाम के विरुद्ध प्रचार में संलग्न थीं। उद्देश्य यह था कि ईसाई जनता इस्लाम और मुसलमानों का नाम सुनना भी पसन्द न करे। इस प्रचार से इस्लाम पर जो झूठे आरोप और इल्ज़ाम लगाए गए उनमें एक यह भी कि इस्लाम एक ख़ूनी धर्म है, वह अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि वे दूसरों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएँ और जो मुसलमान न बने उसकी गर्दन मार दें। पोप और पादरी, लेखक और विद्वान इस झूठे आरोप को एक स्वर में इतनी तत्परता के साथ और इतने दिनों तक दुहराते रहे कि यूरोप का पूरा वातावरण इस प्रचार से भर उठा और सारे ईसाई संसार को विश्वास हो गया कि इस्लाम एक हिंसक और ख़ूनी धर्म है जिसमें दया, प्रेम और मानवता का नाम भी नहीं है।
बाहर के मुसलमानों और भारतवासियों में जो लड़ाई हुई वह इस्लाम के लिए न थी। लड़नेवाले मुसलमानों ने अपने स्वार्थ के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ीं। लेकिन इन लड़ाइयों में जो रक्तपात हुआ उसे इस्लाम के खाते में जमा कर दिया गया, हालाँकि बेचारे इस्लाम का इन लड़ाइयों से दूर का भी सम्बन्ध न था।
भारत में मुसलमानों का राज्य समाप्त हुआ और यूरोप से अंगेज़ी साम्राज्य भारत आया तो वह अपने दूसरे अस्त्र-शस्त्र के साथ वह प्रचार भी लेता आया जो इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध सदियों से यूरोप में फैला हुआ था। हिन्दुस्तान में भी इस्लाम के विरुद्ध घृणा और द्वेष विद्यमान ही था। इसलिए यूरोप से आए हुए इस्लाम विरोधी प्रचार का ख़ूब स्वागत हुआ और धीरे-धीरे इस प्रचार ने स्थायी रूप धारण कर लिया, लेकिन वास्तविकता और सत्य क्या है? इसका जवाब क़ुरआन ही से माँगना चाहिए, क्योंकि वही इस्लाम का मूल आधार है। क़ुरआन में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का आदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा।
क़ुरआन में साफ़ कहा गया-
‘‘धर्म के विषय में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात ग़लत विचारों से अलग छाँटकर रख दी गई है। अब जिस किसी ने बढ़े हुए फ़सादी का इनकार करके अल्लाह को माना, उसने एक मज़बूत सहारा थाम लिया, जो कभी टूटनेवाला नहीं। अल्लाह (जिसका सहारा उसने लिया है) सब कुछ सुनने और जानने वाला है। (क़ुरआन-2:256)
इस आयत का अर्थ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शब्दों में यह है-
‘‘दीन (धर्म) के बारे में किसी तरह का जब्र (ज़बरदस्ती) नहीं, क्योंकि वह दिल के एतिक़ाद (विश्वास) से ताल्लुक़ रखता है और जब्रो-तशद्दुद (हिंसा) से एतिक़ाद नहीं किया जा सकता। बिला शुबह हिदायत (सुपथ) की राह गुमराही (पथभ्रष्टता) से अलग और नुमायाँ (स्पष्ट) हो गई है और जब दोनों राहें लोगों के सामने हैं जिसे चाहें इख़्तियार करें। फिर जो कोई ताग़ूत से इनकार कर दे (यानी सरकशी और फ़साद की कुव्वतों से बेज़ार हो जाए) और अल्लाह पर ईमान लाए तो बिला शुबह उसने (फ़लह व सआदत यानी कल्याण और भलाई की) मज़बूत टहनी पकड़ ली। यह टहनी टूटनेवाली नहीं (जिसके हाथ आ गई वह गिरने से महफ़ूज़ यानी सुरक्षित हो गया) और अल्लाह सब कुछ सुनने और जाननेवाला है।'' (क़ुरआन-2: 256)
इस आयत का जो अर्थ मौलाना आज़ाद ने बयान किया है वही इस्लाम के प्राचीन आचार्यों और विद्वानों ने भी किया है। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़िअल्लाहु अन्हु) हज़रत रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के चचा हज़रत अब्बास के बेटे क़ुरआन के बड़े आलिम थे। उनके द्वारा एक वाक़िआ बयान किया गया है जिसका आशय यह है कि अनसार में से एक आदमी के दो बेटे, ईसाई हो गए थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से अर्ज़ किया कि मेरे बेटे ईसाई मत को छोड़ने पर राज़ी नहीं होते, क्या मै उनको मजबूर कर सकता हूँ । इस पर वह आयत उतरी जो ऊपर उद्धृत की गई है।
अल्लामा इब्ने-कसीर क़ुरआन शरीफ़ के महान आचार्य माने गए हैं, उन्होंने इस आयत की व्याख्या करते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है-
‘‘किसी व्यक्ति को इस्लाम धर्म में दाख़िल होने पर विवश न करो, क्योंकि वह इतना प्रकट और स्पष्ट है और उसकी उक्तियाँ और प्रमाण इतने दिव्य हैं कि किसी व्यक्ति को इसमें प्रविष्ट होने पर बाध्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने जिस शख़्स को हिदायत दी हो और जिसका हृदय सत्य को स्वीकार करने के लिए खोल दिया हो और जिसको ज्ञान चक्षु की ज्योति प्रदान की हो वह स्पष्ट प्रमाण के कारण ख़ुद इस्लाम को स्वीकार करेगा और जिसके दिल को ख़ुदा ने अन्धा कर दिया और जिसकी सुनने और देखने की शक्तियों पर मुहर लगा दी उसका बल और हिंसा द्वारा इस्लाम में दाख़िल होना उसे कोई लाभ न देगा।
मुहर उसी के दिल पर लगाई जाती है जो सत्य के स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसका विरोध ही करता रहता है।
इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) भी क़ुरआन शरीफ़ के प्रसिद्ध टीकाकार गुज़रे हैं। उन्होंने उपर्युक्त आयत के बारे में क़ुरआन के आचार्य अबू-मुस्लिम अस्फ़हानी और कफ़ाल का कथन उद्धृत किया है। उसका आशय यह है-
‘‘ख़ुदा ने दीन के कार्य को ज़ोर-ज़बरदस्ती पर निर्भर नहीं रखा है, बल्कि अधिकार और इख़्तियार पर रखा है। ख़ुदा ने एकेश्वरवाद के प्रमाण ऐसे सन्तोषप्रद और उचित तरीक़े से बयान कर दिए कि बहाना और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही, तो उसने फ़रमाया कि इन तर्कों के स्पष्टीकरण के बाद किसी इनकारी के लिए इनकार पर जमे रहने का कोई कारण बाक़ी नहीं रहा, फिर अब अगर वह ईमान न लाए तो उसको मनवाने की केवल यही एक सूरत बाक़ी रह जाती है कि उसको ज़बरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर किया जाए, मगर यह जाइज़ नहीं है, क्योंकि यह संसार आज़माइश और परीक्षा की जगह है और ज़ोर-ज़बरदस्ती इस्लाम को मानने पर बाध्य करना, परीक्षा और आज़माइश के उद्देश्य को नष्ट कर देता है, उसका प्रमाण ख़ुदा का यह फ़रमान है।''
उसके बाद इसी आशय की क़ुरआन शरीफ़ की और कई आयतों का प्रमाण दिया गया है। अन्त में इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने भी इसी मत की पुष्टि की है।
इस विषय पर जितना लिखा जा चुका है वह पर्याप्त है, फिर भी क़ुरआन की कुछ और आयतें पेश की जाती हैं-
‘‘देखो तुम्हारे पास तुम्हारे प्रभु की ओर से आँख खोल देनेवाले प्रकाश आ गए हैं, अब जो सूझ से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अन्धा बनेगा स्वयं हानि उठाएगा, मैं तुमपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ।'' (क़ुरआन 6:105)
मौलाना आज़ाद ने इस आयत का अर्थ इस प्रकार बयान किया है-
‘‘(देखो) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास इल्म व दौलत (ज्ञान और प्रमाण) की रौशनियाँ आ चुकी हैं। (जहल व नादानी यानी अज्ञानता और नासमझी का कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहा)। अब बस जो कोई देखे और समझे तो (उसका फ़ायदा) ख़ुद उसी के लिए है और कोई (अपनी आँखों से काम न ले और) अन्धा हो जाए तो उसका वबाल (हानि) उसी के सिर आएगा और (ऐ पैग़म्बर ! तुम कह दो) मैं तुमपर पासबान नहीं हूँ (कि जबरन तुम्हारी आँखें खोल दूँ)।''
एक जगह कहा है-
‘‘(ऐ पैग़म्बर !) कह दो कि ऐ लोगो ! तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से सच्चाई तुम्हारे पास आ गई है, सो जो सुपथ ग्रहण करेगा तो वह अपने ही भले के लिए करेगा और जो भटकेगा तो उसकी पथभ्रष्टता उसी के आगे आएगी। मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ (कि ज़बरदस्ती किसी राह में खींच ले जाऊँ और फिर उससे निकलने न दूँ)।'' (क़ुरआन-10:108)
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस आयत की व्याख्या इस प्रकार की है-
क़ुरआन हकीम में तुम जाबजा इस तरह का एलान पाओगे जैसा कि इस आयत में है। उसने पिछले नबियों के जो मवाइज़ (उपदेश) नक़्ल किए है उनमें भी हर जगह ऐसी ही बात पाई जाती है यानी मज़हबी दावत (निमंत्रण) का मामला पूरी तरह समझने-बूझने और समझ-बूझकर इख़्तियार कर लेने का मामला। इसमें न तो किसी तरह की ज़बरदस्ती है, न किसी तरह का लड़ाई-झगड़ा। तुम्हारी भलाई के लिए एक बात कही गई है, अगर समझ में आ जाए तो मान लो न आए तो न मानो। तुम्हारी राह तुम्हारे लिए, हमारी राह हमारे लिए। अगर मान लोगे, अपना ही भला करोगे और न मानोगे तो अपना ही नुक़सान करोगे। हर शख़्स अपने नफ़्स का मुख़्तार (अधिकारी) है, चाहे भलाई की राह चले और भलाई कमाए चाहे बुराई की चाल चले और बुराई कमाए। अगर कोई भलाई की राह चलेगा तो किसी दूसरे को कुछ नहीं देगा कि वह उसके पीछे पड़ जाए। अगर कोई बुराई की चाल चलेगा तो किसी दूसरे का नुक़सान नहीं कर देगा कि वह उससे बिगड़ने लगे। अपनी-अपनी राह है और अपनी-अपनी कमाई।
‘‘जिसने अच्छे काम किए उसने अपने ही लिए किए और जिसने बुरे काम किए उसकी हानि उसी पर होगी और तेरा परवरदिगार अपने बन्दों पर ज़ुल्म करनेवाला नहीं है।'' (क़ुरआन-41:46) साथ ही स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई की तरफ़ बुलानेवाले की हैसियत क्या है-
मैं दाई (दावत देने वाला) और मुज़क्किर (उपदेशकर्ता) हूँ, कुछ तुम पर वकील नहीं हूँ। यानी मेरा काम यह है कि नसीहत की बात सुझा दूँ, यह नहीं है कि निगहबान बन कर तुम पर मुसल्लत हो जाऊँ और समझूँ कि मुझे तुम्हारी हिदायत की ठेकेदारी मिल गई है। दूसरी जगह पैग़म्बरे-इस्लाम को सम्बोधित करते हुए यही मतलब यूँ अदा किया है-
‘‘तू उन लोगों पर एक हाकिमे-जाबिर की तरह मुसल्लत नहीं है कि बलपूर्वक और ज़बरदस्ती बात मनवा दे।'' और फ़रमाया-
‘‘तुम्हें इन लोगों पर दारोग़ा बनाकर नहीं बैठा दिया है कि ये मानें या न मानें लेकिन तुम इन्हें राहे-हक़ पर चलाने के ज़िम्मेदार हो।''
अनेकों स्थानों पर विभिन्न अन्दा़ज़ में यह बात वाज़ेह कर दी है कि पैग़म्बर का मक़ाम इसके सिवा कुछ नहीं है कि सच्चाई की पुकार बुलन्द करनेवाला है, सत्य का सन्देश पहुँचा देनेवाला है, नसीहत की बात समझा देनेवाला है, ईमान और भले कर्मों के परिणाम की ख़ुशख़बरी (सन्देश) देता और इनकारों तथा कुकर्म के अंजाम से ख़बरदार कर देता है।
सोचिए क्या इससे ज़्यादा साफ़, बेलाग और अम्न व सलामती की कोई राह हो सकती है ? अगर दुनिया ने दावते-हक़ की यह रूह (आत्मा) समझ ली होती, तो क्या यह मुमकिन था कि कोई इनसान महज़ इख़्तिलाफ़े-एतिक़ाद व अमल, (विश्वास और कर्म) की बिना पर लड़ता ? लेकिन मुसीबत यह है कि इनसान के जु़ल्म और सरकशी ने भी इस हक़ीक़त को स्वीकार नहीं किया और यही बात सारे झगड़ों की जड़ बन गई है । क़ुरआन ने पिछली दावतों (पैग़म्बरों की शिक्षाओं) की जिस क़द्र सरगुज़शतें (वृत्तांत) बयान की हैं, उन्हें जाबजा पढ़ो, हर जगह देखोगे कि झगड़े की जड़ यही थी। ख़ुदा के रसूलों का हमेशा यही एलान हुआ कि हम नसीहत करनेवाले हैं, मानना न मानना तुम्हारा काम है, अगर नहीं मानते तो तुम अपनी राह चलो, हमें अपनी राह चलने दो और देखो नतीजा क्या निकलता है। लेकिन उनके मुनकिर (इनकारी) कहते थे कि न तो हम तुम्हारी बात मानेंगे न तुम्हें तुम्हारी राह चलने देंगे....।
इस्लाम और उसके मुनकिरों (इनकारियों) में जो झगड़ा शुरू हुआ वह भी तमामतर यही था। क़ुरआन कहता था कि मेरी राह तबलीग़-तज़कीर (प्रचार और उपदेश) की है। मुख़ालिफ़ कहते थे कि हमारी राह जब्र व तशद्दुद (ज़ोर-ज़बरदस्ती और हिंसा) की है। क़ुरआन कहता कि अगर मेरी बात समझ में आए तो मान लो, न समझ में आए तो माननेवालों को राह चलने दो। वे कहते कि हमारी बात तुम्हारी समझ में आए या न आए तुम्हें माननी ही चाहिए, नहीं मानोगे तो जबरन मनवाएँगे।
हक़ीक़त यह है कि क़ुरआन ने इस आयत में और उसकी हममानी आयत में जो बात कह दी है, अगर दुनिया उसे समझ लेती तो मानवजाति की वह तमाम खूँरेज़ियाँ (रक्तपात) जो फ़िक्रो अमल के इख़तिलाफ़ से पैदा हुई एकदम ख़त्म हो जातीं और आजकल भी जो इस क़द्र झगड़े हो रहे हैं वे भी ख़त्म हो जाएँ। ग़ौर कीजिए सारे झगड़ों की असली बुनियाद क्या है। यही है कि लोग समझाने-बुझाने और ज़ोर-ज़बरदस्ती में फ़र्क़ नहीं करते। क़ुरआन कहता है कि दोनों में फर्क़ करो, तज़कीर की राह यह हुई कि जो बात ठीक समझते हो उसकी दूसरों को भी नसीहत करो मगर सिर्फ़ तऱगीब दो, इससे आगे न बढ़ो यानी यह बात न भूल जाओ कि पसन्द करने न करने का हक़ दूसरों को है, तुम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। ज़ोर-ज़बरदस्ती और सीनाज़ोरी यह हुई कि डण्डा लेकर खड़े हो जाओ और जो कोई तुमसे मुत्तफ़िक़(सहमत) न हो, उसके पीछे पड़ जाओ। गोया ख़ुदा ने तुम्हें लोगों की हिदायत और गुमराही का ठेकेदार बना दिया है जबकि क़ुरआन साफ़-साफ़ कहता है कि ख़ुदा के रसूलों का मनसब (पद) भी तज़कीर व तबलीग़ के अन्दर महदूद (सीमित) था, हाँलाकि वे अल्लाह की तरफ़ से नियुक्त थे, तो ज़ाहिर है कि वह किसी दूसरे इनसान के लिए यह कब गवारा (सहन) कर सकता है कि वह वकील, दारोग़ा और ज़ोर-ज़बरदस्ती करनेवाला बन जाए।
वास्तव में इनसान के कर्म के सभी क्षेत्रों में असली सवाल सीमाओं ही का है और हर जगह इनसान ने उसी में ठोकर खाई है। यानी हर बात की जो हद है वह उसके अन्दर नहीं रहना चाहता। दो हक़ हैं और दोनों को अपनी-अपनी हदों के अन्दर रहना चाहिए। एक हक़ तज़कीर व तबलीग़ का है, एक पसन्द व क़ुबूलियत का है। हर इनसान को इसका हक़ है कि जिस बात को दुरुस्त समझता है उसे दूसरों को भी समझाए, लेकिन उसे इसका हक़ नहीं है कि दूसरों के हक़ से इनकार कर दे, यानी यह बात झुठला दे कि जिस तरह उसे एक बात के मानने न मानने का हक़ है, वैसा ही दूसरे को भी मानने न मानने का हक़ है और एक व्यक्ति दूसरे के लिए ज़िम्मेदार नहीं ।
हमने यहाँ जिस बात को हक़ कहा है, क़ुरआन उसे हर इनसान का फ़र्ज़ क़रार देता है यानी वह कहता है कि जिस बात को तुम सच समझते हो तुम्हारा फ़र्ज़ हैकि उसे दूसरों तक पहुँचाओ। अगर इसमें कोताही की तो ख़ुदा के आगे जवाबदेह होगे। लेकिन साथ ही याद रखो, फ़र्ज़ तज़कीर व तबलीग़ है, ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं और जवाबदेही इसमें है कि तुमने तबलीग़ की या नहीं, इसमें नहीं है कि दूसरों ने माना या नहीं। ग़ौर करो, क़ुरआन ने किस दर्जा न्याय के साथ मामले के दोनों पहलुओं की हिफा़ज़त की है और फिर उसकी हदबन्दियों की रेखा खींच दी है। उसने एक तरफ़ तज़कीर व दावत (उपदेश और आवाहन) पर ज़ोर दिया ताकि हक़ की मांग और स्थापना की रूह कुंठित न हो, दूसरी तरफ़ इनसान की शख़्सी आज़ादी (व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता) भी महफ़ूज़ कर दी कि ज़ोर-ज़बरदस्ती और हिंसा से बेजा हस्तक्षेप न कर सके। हदबन्दी की यही हद है जो यहाँ बीच की हालत क़ायम रखती है। उसे अपनी जगह से इधर-उधर कर दो तो दोनों में से कोई बात ज़रूर ग़लत हो जाएगी। अगर दावत व तज़कीर का क़दम आगे बढ़ेगा तो आस्था और विचार की व्यक्तिगत आज़ादी बाक़ी नहीं रहेगी, अगर व्यक्तिगत आज़ादी के मुतालबे में बढ़ जाओगे तो हक़ व अदालत के तलब व क़ियाम की व्यवस्था बिगड़ जाएगी यानी सत्य और न्याय की मांग और स्थापना की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी।
क़ुरआन की बहुत-सी बातों की तरह इस बात के समझने में भी दुनिया ने बड़ी देर लगाई और तारीख़ को बारह सदियों तक इस बात का इन्तिज़ार करना पड़ा कि एक इनसान दूसरे इनसान को महज़ इख़्तिलाफ़े अक़ाइद (विश्वास-भेद) की बिना पर ज़िब्ह (वध) न करे और इतनी बात समझ ले कि तज़कीर और तौकील में फ़र्क़ है। अब डेढ़ सौ वर्ष से यह बात दुनिया के अक़ली मुसल्लमात (बौद्धिक सत्य) में से समझी जाती है लेकिन उसे मालूम नहीं कि उसके एलान की तारीख़ (इतिहास) अमेरिका और फ़्रांस के एलान हुकूक़े इनसानी (मावन अधिकार) से शुरू नहीं हुई है बल्कि इससे बारह सौ वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। (तर्जुमानुल क़ुरआन, भाग-2, पृष्ठ 172 से 174 तक)
इस विषय की इतनी विस्तृत और गम्भीर विवेचना के बाद अब किसी को इस बात के मानने में सन्देह बाक़ी नहीं रह सकता कि इस्लाम में ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाज़त मौजूद नहीं है।
इस्लामी युद्ध का उद्देश्य
यह बात तो भली-भाँति सिद्ध हो गई कि इस्लाम में ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की अनुमति नहीं है फिर भी जो भ्रम और सन्देह एक युग से जड़ पकड़े हुए है उसके कारण कुछ लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि क़ुरआन में जो युद्ध के आदेश हैं, उनका उद्देश्य क्या है और हज़रत मुहम्मद और उनके सहाबा के समय में जो लड़ाइयाँ हुईं वे क्यों हुईं ?
जब यह बात सिद्ध हो गई कि इस्लाम ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाज़त नहीं देता तो सिरे से यह भ्रम और सन्देह ही अनुचित है कि क़ुरआन में युद्ध के आदेश हैं और इस्लाम के पैग़म्बर और उनके सहाबा के काल में लड़ाईयाँ हुई हैं तो वे लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान ही बनाने के लिए हुई होंगी। हर विवेकशील व्यक्ति स्वयं सोच सकता है कि इस्लामी लड़ाइयों का उद्देश्य कुछ और ही होगा और यही तथ्य भी है।
हम यहाँ दो प्रमुख विद्वानों की रायें देना आवश्यक समझते हैं जो हमारे विषय से सम्बन्ध रखती हैं।
प्रसिद्ध अंग्रेज़ महिला मिसे़ज एनी बेसेंट, जो हिन्दुस्तान के इतिहास में अपना एक विषेश स्थान रखती हैं, अपने एक लेक्चर में कहती हैं-
‘‘हज़रत मुहम्मद साहब देश त्यागकर मदीना पहुँचते हैं और वहाँ के लोग उनसे अति प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हैं और वे वहाँ के शासक बना दिऐ जाते हैं। उनके दुश्मन मक्का से उनका पीछा करते हैं। हज़रत के साथियों की संख्या बहुत कम है और दुश्मनों की सेना बहुत अधिक है। अंततः दोनों के बीच लड़ाई होती है और यह युद्ध ‘बद्र की लड़ाई' के नाम से प्रसिद्ध है। पैग़म्बर साहब चिल्लाकर कहते हैं- ‘ऐ ख़ुदा ! अगर आज यह छोटी-सी टोली तबाह हो गई तो फिर (दुनिया में) तेरी सच्ची उपासना करनेवाला कोई प्राणी बाकी़ न रहेगा।' लड़ाई घमासान की होती है और हज़रत की जीत हो जाती है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हज़रत के साथ है। यही हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की पहली लड़ाई है जो रक्षा के उद्देश्य से लड़ी गई। पैग़म्बर साहब सहृदय और दयालु थे। उनके शत्रु उन्हें ‘स्त्री हृदय रखनेवाला' कहकर पुकारते थे। लेकिन अब वह प्राइवेट व्यक्ति की स्थिति में नहीं हैं कि वह उन समस्त अपराधों को क्षमा करदे जो उनके विरुद्ध किए गए हैं, वह एक राज्य के शासक हैं, एक सेना के सेनाध्यक्ष हैं और उनपर उन साथियों के भी कुछ अधिकार है, जिन्होंने उन पर भरोसा कर रखा है। वे दिन आ रहे हैं जबकि प्राइवेट व्यक्ति के रूप में वह अपराधों को क्षमा कर देंगे। लेकिन एक शासक के रूप में उनके लिए दण्ड देना अनिवार्य होगा। और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ऐसे नहीं है कि केवल भावनावश कोई काम कर जाएँ।
बद्र की विजय के बाद सिर्फ़ दो आदमियों को प्राणदण्ड दिया गया और अरब की रस्म के विरुद्ध क़ैदियों के साथ हज़रत की आज्ञानुसार अत्यन्त दयापूर्ण व्यवहार किया गया। मुसलमान उन्हें रोटी खिलाते थे और अपने लिए सिर्फ़ खजूरें रखते थे।'' (मासिक निज़ामुलमशाइख़,दिल्ली, जमादिलऊला 1934)
प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर एडवर्ड गिब्बन लिखते हैं-
‘‘प्राकृतिक नियम के अनुसार हर आदमी को हक़ है कि हथियारों द्वारा अपने प्राण और धन की रक्षा करे, अपने दुश्मनों के अत्याचार और दमन का बलपूर्वक प्रतिकार करे या रोके और उनके साथ दुश्मनी को बदले की उचित सीमा तक प्रसारित करे। अरबों के स्वतन्त्र समाज में क्या प्रजा होने के विचार से और क्या एक नगर के निवासियों के पारस्परिक बरताव के विचार से लोगों के कर्तव्य में एक कमज़ोर-सी रोक थी और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अपने देशवासियों की बेइनसाफ़ी के कारण अपना सन्देश पहुँचाने से, जो सर्वथा शान्तिपूर्ण और जनता की भलाई पर निर्भर था, वंचित किया गया और स्वदेश से निकाला गया था। एक स्वाधीन जाति की स्वीकृति ने मक्का के इस शरणार्थी को शासक के पद पर पहुँचा दिया और उसको उचित रूप से लोगों के साथ संधि करने और शत्रुओं के आक्रमणों को दूर करने या उन पर आक्रमण करने का अधिकार प्राप्त हो गया।''
‘‘.......शुभचिन्तक बुद्धि विश्वास कर सकती है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का वास्तविक उद्देश्य शुद्ध और संसार का सच्चा कल्याण था। मगर एक ऐसे पैग़म्बर से जो मनुष्य था । यह नहीं हो सकता कि वह ऐसे हठी विरोधियों को सहन करे जो उसके दावों का इनकार और उसके तर्को का अपमान करें और उसके प्राण का कष्ट पहुँचाएँ। वह अपने निजी दुश्मनों को तो क्षमा कर सकता है, मगर ईश्वर के शत्रुओं से उचित रूप से दुश्मनी रख सकता है.....।'' (एजाज़ुत्तंज़ील, पृष्ठ 450)
प्रसिद्ध अंग्रेज़ इतिहासकार मिस्टर टामस कारलायल लिखते हैं-
‘‘हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अब तक अपने धर्म के प्रचार के लिए सिर्फ़ वाज़ और उपदेश का तरीका अपना रखा था, लेकिन अब जो अन्यायपूर्ण ढंग से उनको स्वदेश से निकाला गया और अत्याचारी लोगों ने केवल इतना ही नहीं किया कि उनके सच्चे अलौकिक सन्देश के सुनने में अनिच्छा प्रकट की जो उनके हृदय की आवाज़ थी, बल्कि जब वह इस सन्देश के सुनाने से चुप न हुए तो उनकी जान के दुश्मन बन गए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक वीर अरब की तरह अपनी रक्षा का निश्चय किया।.... हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को दस बरस युद्ध, कठिन श्रम और संधर्ष में बिताना पड़ा और उसका जो कुछ परिणाम हुआ उससे हम सब अवगत हैं।''
सच्ची बात यह है कि इस्लाम केवल ईश-उपासना और कुछ जातीय रीति-रिवाज तक सीमित नहीं है। यह एक सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्था है जिसे आप चाहें तो ईश्वरवाद कह सकते हैं यानी ईश्वरीय आदेशों और नियमों पर आधारित कोई जीवन-व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसमें युद्ध आवश्यक और अनिवार्य न हो। ऐसी कोई व्यवस्था न बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित रह सकती है और न भीतरी दुष्टों और द्रोहियों से। और न वह अपने उद्देश्य और सिद्धान्त को सफल बना सकती है, यदि इसके साथ युद्ध-शक्ति और युद्ध-प्रबन्ध न हो। जिस जीवन-व्यवस्था को आप स्वयं मानते हों उसी के सम्बन्ध में सोच लीजिए, क्या वह युद्ध शक्ति के बिना अपने उद्देश्य और सिद्धान्त में सफल हो सकती है? और सफल होकर स्थिर और बाक़ी रह सकती है? नहीं, कदापि नहीं, यह असम्भव है।
इस्लाम को अपने आदि काल में बड़े-बड़े दुखों और संकटों से सामना हुआ। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके मुट्ठी भर सहाबा अपने विश्वास, सिद्धान्त और उद्देश्य का पालन करने और दूसरों को इसका सन्देश देने के सिवा और कुछ नहीं करते थे, लेकिन इतने ही पर सारा नगर, सारा देश, और सारी जाति आप लोगों की शत्रु बन गई। महीना दो महीना नहीं, साल दो साल नहीं, पूरे बारह साल तक मुसलमानों पर निरन्तर अत्याचार होते रहे। निश्चय कर लिया गया था कि मुसलमानों को कुचल डाला जाए और इस्लाम को मिटा दिया जाए। यहाँ तक कि हज़रत पैग़म्बरे-इस्लाम और मुसलमान अपनी जन्म-भूमि और अपना सब कुछ छोड़कर मक्का से मदीना चले गए। इतने पर भी इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध शत्रुता और अत्याचार का सिलसिला जारी ही रहा। जो मुसलमान अपनी बेबसी के कारण मक्का ही में रह गए थे वे और ज़्यादा सताए जाने लगे। और जो मुसलमान मदीना चले गए थे उनपर भी आक्रमण होने लगे। तब कहीं जाकर मुसलमानों को रक्षा के लिए युद्ध करने की अनुमति मिली।
युद्ध की अनुमति की पहली आयत यह है-
‘‘अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वे उत्पीड़ित हैं। और अल्लाह को निश्चय ही उनकी सहायता की सामर्थ्य प्राप्त है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक़ निकाल दिए गए केवल इस दोष पर कि वे कहते थेः ‘हमारा प्रभु अल्लाह है'। यदि अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता न रहे तो आश्रम और गिरजा और उपासनाग्रह और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है, सब ढा दी जाएँ। अल्लाह अवश्य उन लोगों की सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेंगे। अल्लाह बड़ा बलवान और प्रभुत्वशाली है।'' (क़ुरआन-2:239-40
इसका अर्थ मौलाना आज़ाद ने इस प्रकार बयान किया है-
‘‘जिन (मोमिनों) के ख़िलाफ़ ज़ालिमों ने जंग कर रखी है अब उन्हें भी (इसके जवाब में) जंग की रुख़्सत (अनुमति) दी जाती है, क्योंकि उन पर सरासर ज़ुल्म हो रहा है और अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर क़ादिर (समर्थ) है। ये वे मज़लूम (अत्याचार से पीड़ित) हैं जो बगै़र किसी हक़ के अपने घरों से निकाल दिए गए, उनका कोई जुर्म न था, अगर था तो सिर्फ़ यह कि वे कहते थे, हमारा परवरदिगार अल्लाह है। और देखो, अल्लाह कुछ लोगों के हाथों कुछ लोगों को हटाता न रहता (और एक गिरोह को दूसरे गिरोह पर ज़ुल्म व तशद्दुद करने के लिए बेरोक छोड़ देता) तो किसी क़ौम की इबादतगाह (उपासना-गृह) ज़मीन पर महफ़ूज़ (सुरक्षित) न रहती । ख़ानक़ाहें (मठ), गिरजे, इबादतगाहें, मस्जिदें जिनमें इस अधिकता के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, सब कभी के ढाए जा चुके होते। (याद रखो) जो कोई अल्लाह (की सच्चाई) की हिमायत करेगा ज़रूरी है कि अल्लाह भी उसकी मदद फ़रमाए। कुछ संदेह नहीं वह यक़ीनन ताक़त रखनेवाला और सब पर ग़ालिब (प्रभुत्व प्राप्त) है।''
‘‘ये (मज़लूम मुसलमान) वे हैं कि अगर हमने उन्हें ज़मीन में साहिबे इक़्तिदार (सत्ता-स्वामी) कर दिया (यानी उनका हुक्म चलने लगा) तो वे नमाज़ की व्यवस्था का़यम करेंगे। ज़कात अदा करने में सरगर्म होंगे, नेकियों का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकेंगे और तमाम बातों का अंजामेकार (अन्तिम परिणाम) अल्लाह ही के हाथ है।'' (क़ुरआन-22:41)
मौलाना आज़ाद ने इन आयतों की व्याख्या इस प्रकार की है-
‘मुसलमानों को इजाज़त दी है कि वे अपनी रक्षा में हथियार उठा सकते हैं। इस् पर सारे उलमा एक मत हैं कि यह पहली आयत है जो जंग की इजाज़त के बारे में उतरी है।''
इससे पहले मक्का के क़ुरैश (मक्का की प्रसिद्ध जाति) का यह ज़ुल्म बयान कर दिया था कि उन्होंने मुसलमानों पर हज की राह बन्द कर दी है, जिसका उन्हें कोई हक़ नहीं । अब यहाँ साफ़-साफ़ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि जंग की इजाज़त की वजह क्या है, फ़रमाया-
‘‘मुसलमान मज़लूम हैं और मज़लूम का हक़ है कि ज़ालिम के मुक़ाबले में अपना बचाव करे। यह मज़लूम तेरह वर्ष तक मक्का के क़ुरैश के अत्याचार और हिंसा का निशाना रहे, आख़िर में स्वदेश त्याग करने को मजबूर हुए। लेकिन विदेश में भी चैन से न बैठने दिया गया। उनके ख़िलाफ़ जंग का एलान कर दिया गया, आख़िर उनका क़ुसूर क्या था । सिर्फ़ यह कि वे कहते थे ‘रब्बुनल्लाह' यानी "हमारा रब अल्लाह है।" हम अपने यक़ीन के मुताबिक़ अपने परवरदिगार को याद करना चाहते हैं, हम दूसरों को मजबूर नहीं करते कि हमारा धर्म क़बूल कर लें लेकिन दूसरे हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम अपनी आस्था और विश्वास से अलग हो जाएँ।
इसके बाद स्पष्ट किया कि यह मज़लूमों का क़ुदरती हक़ है अगर वे इस हक़ से महरूम (वंचित) कर दिए जाएँ तो दुनिया में अत्याचारी इनसानों की ज़ुल्म-ज़्यादतियों का प्रतिकार करने का कोई सम्मान बाक़ी न रहे। जिस गिरोह की बन पड़े दूसरे गिरोह के विश्वास और कर्म की आज़ादी हमेशा के लिए पामाल कर दे। चुनाँचे फ़रमाया-
‘‘यहाँ अल्लाह ने एक जमाअत के हाथों दूसरी जमाअत के अत्याचार और हिस्सा को मिटाने की व्यवस्था क़ायम कर रखी है। अगर एक के द्वारा दूसरे की रक्षा करने का सिलसिला न होता तो दुनिया में ख़ुदापरस्ती का ख़ातिमा (अन्त) हो जाता। किसी गिरोह की इबादतगाह इनसानी जुल्मो-ज़्यादती के हाथों महफ़ूज़ न रहती।''
क़ुरआन के नज़दीक मुसलमानों के इक़्तिदार व हुकूमत का असली मक़सद क्या था? फ़रमाया-‘‘इन मज़लूम मुसलमानों के क़दम जम गए तो ये क्या करेंगे? यानी धरती पर सत्ता की प्राप्ति को किन उद्देशों के लिए काम में लाऐंगे? इसलिए कि नमाज़ क़ायम करें, ज़कात अदा करें, नेकी का हुक्म दें, बुरायों से रोकें और अत्याचार और अपकर्म (बुरे काम) की जगह न्याय, सत्कर्म और पुण्य का राज स्थापित हो जाए।'' (तर्जुमानुल क़ुरआन, भाग 2, पृष्ठ 511-512)
इसी तरह की एक और आयत है जिससे इस्लामी जंग का उद्देश्य सामने आता है, फ़रमाया गया है-
‘‘और (मुसलमानो!) तुम्हें क्या हो गया कि अल्लाह की राह में जंग नहीं करते, हालाँकि कितने ही बेबस मर्द हैं कितनी ही औरतें हैं, कितने ही बच्चे हैं जो (ज़ालिमों के जु़ल्म से आजिज़ आकर) फ़रियाद कर रहे हैं कि ऐ हमारे पालनकर्ता! हमें इस बस्ती से निकाल (कर मुक्ति दे) जिसके बसनेवाले बड़े ही अत्याचारी हैं और अपनी तरफ़ से किसी को हमारा हिमायती बना दे और अपनी ही ओर से किसी को हमारा सहायक बना दे।'' (क़ुरआन 4:75)
मौलाना आज़ाद ने इस आयत की व्याख्या इस तरह की है-
‘‘यहाँ यह हक़ीक़त भी स्पष्ट कर दी कि क़ुरआन ने जंग का हुक्म इसलिए नहीं दिया है कि मुसलमान दूसरों पर चढ़ दौड़ें, बल्कि इसलिए कि मज़लूमों और बेकसों (अत्याचार पीड़ितों और निस्सहाय लोगों) की हिमायत करें और उन्हें ज़ालिमों के पंजे से मुक्ति दिलाएँ। इसी लिए वह बार-बार कहता है कि अल्लाह की राह में लड़ो, यानी अपनी नफ़सानी ख़ाहिशों (मनोकामनाओं) के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के अद्ल व इनसाफ़ के क़ियाम (स्थापना) के लिए लड़ो।'' (तर्जुमानुल क़ुरआन, प्रथम भाग पृ0 379)
कुछ मुख्य आयतों को लेकर इस्लाम के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया गया है विशेष कर स्वामी दयानन्द की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इस्लाम के प्रति बड़ा भ्रम फैलाया गया है। कहा गया है कि क़ुरआन ने मुसलमानों को आज्ञा दी है कि काफ़िरों को जहाँ पाओ उनकी गर्दन मार दो। इस दुष्प्रचार की वास्तविकता क्या है? इसका स्पष्ट हो जाना भी आवश्यक है। पवित्र क़ुरआन में है-
‘‘(मुसलमानो!) जो लोग तुमसे युद्ध करते हैं, अल्लाह की राह में तुम भी उनसे युद्ध करो। मगर (देखो) किसी प्रकार की ज़्यादती न करना। निस्संदेह अल्लाह ज़्यादती करनेवालों को प्रिय नहीं रखता। (मक्का के) जिन लोगों ने तुमसे युद्ध छेड़ रखा है, उनको जहाँ पाओ क़त्ल करो और जिस जगह से उन्होंने तुमको निकाला है तुम भी (युद्ध करके) उनको वहाँ से निकाल दो और फ़ितना (धर्म में विघ्न-बाधा डालना) रक्तपात से भी अधिक भयंकर है और शत्रु जब तक स्वयं प्रतिष्ठावाली मस्जिद (काबा) के क्षेत्र में तुमसे युद्ध न करे तुम उसके क्षेत्र में उनसे युद्ध न करना। हाँ, अगर वे युद्ध में पहल करें तो तुम भी उनसे युद्ध करो, न माननेवालों (की ज़्यादती) का यही बदला है। फिर यदि वे (युद्ध से) रुक जाएँ तो (तुम भी रुक जाओ) निस्संदेह अल्लाह बहुत बड़ा क्षमाकर्ता और दयावान है। (सारांश यह कि) जब तक फ़ितना (धर्म मे विघ्न-बाधा) मिट न जाए धर्म अल्लाह के लिए (स्वतन्त्र) न हो जाए, युद्ध करते रहो, फिर अगर वे (युद्ध से) रुक जाएँ तो तुम भी रुक जाओ, लड़ाई तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अत्याचारी हैं।''(क़ुरआन, 2:190-193)
युद्ध सम्बन्धी ये विशेष आयते हैं, इसलिए गै़र-मुस्लिम भाई इन पर ध्यान पूर्वक विचार करें। मुसलमानों को विधर्मियों से केवल विधर्मी होने के कारण युद्ध करने की अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि ऐसे विधर्मियों से युद्ध करने की अनुमति दी गई है जो इस्लाम को सहन नहीं कर सकते थे, जो मुसलमानों के शत्रु थे और मुसलमानों को समाप्त कर देना चाहते थे।
मक्का के विधर्मी महाईश-दूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को सत्य-धर्म (इस्लाम) का प्रचार नहीं करने देते थे। आपका अपमान करते थे। काबा में नमाज़ नहीं पढ़ने देते थे। मिथ्या प्रचार करके आपके विरुद्ध लोगों को बहकाते और भड़काते थे जो आप पर एवं मुसलामानों पर भयंकर अत्याचार करते थे, जिन्होंने आपका और आपके परिवार का बहिष्कार किया, जो तीन वर्ष तक जारी रहा। बहिष्कार भी ऐसा निर्दयतापूर्ण था कि बहिष्कृत परिवार तक मुट्ठी-भर खाद्य-सामग्री भी नहीं पहुँच पाती थी। बच्चे भूखों मरते थे, रोते-बिलखते थे। जीवन-रक्षा के लिए वृक्षों के पत्ते और सूखे चमड़े भिगोकर खाने पड़ते थे, कितने हृदयहीन थे विरोधी! उद्देश्य यह था कि महाईश-दूत सत्य-धर्म का प्रचार त्याग करने को मजबूर हो जाएँ, शत्रु इस प्रकार एक दो-वर्ष नहीं 13 वर्ष क विरोध तथा अत्याचार करते रहे। अन्त में उन्होंने महाईश-दूत की हत्या करने की योजना बनाई। रात्रि में आपका घर घेर लिया कि आप बाहर निकलें तो आपकी हत्या कर दें।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ईशदूत थे, ईश्वर आपका रक्षक था। आप शत्रुओं के बीच से निकले और मदीना पहुँच गए, यहाँ के निवासी मुसलमान हो चुके थे और उनके सरदारों से यह तय हो चुका था कि आप मक्का त्याग करके मदीना चले आएँ।
अत्याचारी इतने पर ही सन्तुष्ट एवं शान्त न हुए। उन्होंने मदीना पर चढ़ाई कर दी। इन आयतों में ऐसे ही विधर्मी शत्रुओं से युद्ध करने की आज्ञा दी गई है। क्या यह आज्ञा अनुचित है?
ऐसे शत्रुओं से भी युद्ध की आज्ञा देते हुए मुसलमानों को चेतावनी दी गई कि तुमको युद्ध की अवस्था में भी ज़्यादती न करनी चाहिए अर्थात् तुम्हारा कोई काम अत्याचारपूर्ण न हो। याद रखो, ईश्वर ज़्यादती करनेवाले को पसन्द नहीं करता।
इस ज़्यादती का तात्पर्य भी समझ लेना चाहिए। ज़्यादती की मनाही के अन्तर्गत हर वह कार्य और व्यवहार आ जाता है जो अनुचित, अनैतिक तथा न्याय-विरुद्ध हो। मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि उन लोगों से युद्ध निषिद्ध है जो तुम्हारे धर्म में विघ्न-बाधा नहीं डालते। स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा आहतों पर हाथ न उठाना, खेतियों और पशुओं को निरर्थक हानि न पहुँचाना, अपनी शारीरिक शक्ति का वहीं प्रयोग करना जहाँ वह अनिवार्य हो और उसी सीमा तक करना जितने की आवश्यकता हो, इससे अधिक नहीं। इस आदेश का उद्देश्य यह था कि इस्लाम से पहले अरब निवासी यह सब अमानुषिक क्रूर कार्य करते थे।
जब शत्रु को शान्ति का विचार ही न हो, वह लड़ने ही पर कटिबद्ध हो तो ऐसी अवस्था में लड़ने के सिवा मार्ग ही कौन-सा रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ भी उससे सामना हो जाए, लड़ो और जहाँ से भी उसने तुमको निकाला है तुम उसे निकाल दो।
रक्तपात कोई प्रिय कार्य नहीं है, परन्तु जब शत्रु धर्म में विघ्न-बाधा डालें, विद्या, ज्ञान, उक्ति और प्रमाण द्वारा अपना विचार सत्य सिद्ध करने के स्थान पर बलपूर्वक लोगों को सत्य-मार्ग से रोकें और उनपर अपना विचार तथा अपना विश्वास अनोधिकार लादना चाहें तो यह हत्या से भी अधिक हैवानी काम है। ऐसे अत्याचारी शत्रुओं से युद्ध करना कल्याणकारी है।
काबा के क्षेत्र में युद्ध निषिद्ध है, परन्तु मक्का के विधर्मी अपनी शक्ति के घमण्ड में काबा की मर्यादा का भी विचार नहीं रखते थे। इसलिए मुसलमानों से कहा गया कि तुम स्वयं तो काबा के क्षेत्र के अन्तर्गत युद्ध में पहल न करो, परन्तु शत्रु न मानें, लड़ पड़ें तो फिर तुम भी उनसे लड़ो।
ऐसे विधर्मी अत्याचारी तथा दुष्ट शत्रुओं के सम्बन्ध में भी मुसलमानों से कहा गया है कि यदि वे युद्ध का परित्याग कर दें तो ईश्वर बड़ा क्षमाशील तथा दयावान है। इस पवित्र शैली में मुसलमानों को नैतिकता की उच्चकोटि की बात बताई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता और दयालुता ईश्वर का महान गुण है। इसलिए मुसलमानों में भी यह गुण विद्यमान होना चाहिए। यदि शत्रु युद्ध का परित्याग कर दें तो फिर प्रतिकार की भावना से तुम्हारा लड़ना उचित नहीं। यदि शत्रु अपना हाथ रोक ले तो तुम भी अपना हाथ रोक लो।
अन्त में, फिर कहा गया है कि तुम्हारी लड़ाई तो धर्म के मार्ग से बाधा को हटाने के लिए है। अतः तुमको उसी समय तक लड़ना चाहिए, जब तक बाधा हट न जाए और जब बाधा हट जाए और धर्म ईश्वर के लिए हो जाए अर्थात् उसकी भक्ति, उपासना और आज्ञा के पालन में कोई बाधा न रह जाए, शत्रु युद्ध से रुक जाए तो तुम भी हाथ रोक लो, लड़ाई का विधान तो अत्याचारियों ही के लिए है।
ग़ैर-मुस्लिम भाई विचार करें कि युद्ध-सम्बन्धी ऐसा नियम किस धर्म, किस विधान अथवा किस सामरिक शास्त्र में है; विरोधियों ने ऐसी पवित्र शिक्षा को भ्रष्ट प्रचार करके क्या से क्या बना दिया? इसी आशय की एक आयतें दूसरे स्थान पर भी हैं। स्वामी दयानन्द जी ने इस आयत पर भी आक्षेप किया है। आयत इस प्रकार है-
‘‘ऐ मुसलमानो ! इन विधर्मियों से लड़ो, यहाँ तक कि फ़ितना (धर्म में विघ्न-बाधा) बाकी़ न रहे और धर्म पूर्ण रूप से अल्लाह के लिए हो जाए। फिर यदि वे फ़ितना से रुक जाएँ तो उनके कार्यों को देखनेवाला अल्लाह है। और यदि वे न मानें तो जान रखो कि अल्लाह संरक्षक है और वह बहुत-ही अच्छा संरक्षक और बहुत-ही अच्छा सहायक है।''
(क़ुरआन-8:39-40)
इन आयतों का भी वही उद्देश्य है जो सूरा बक़रा की ऊपर की आयतों का है। मुसलमानों को सत्य-धर्म की रक्षा तथा संमार्ग से विघ्न-बाधा को हटाने के अतिरिक्त किसी भौतिक उद्देश्य से युद्ध करने की अनुमति नहीं है। हम अन्त में गै़र-मुस्लिमों से सम्बन्धित पवित्र क़ुरआन की दो आयतें पेश करते हैं। इनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि गै़र-मुस्लिमों के विषय में इस्लाम का सिद्धान्त क्या है-
‘‘(मुसलमानो!) जिन लोगों ने तुम से धर्म के सम्बन्ध में युद्ध नहीं किया, और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला उनके साथ भलाई और न्यायसंगत व्यवहार करने से खु़दा तुमको मना नहीं करता, इसके विपरीत खु़दा तो न्याय करनेवालों से प्रेम करता है। खु़दा तुमको उन्हीं लोगों से मित्रता कि मनाही करता है जिन्होंने तुमसे धर्म के सम्बन्ध में युद्ध किया और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हें निकालने में सहायता की हो और जो लोग ऐसों से मित्रता करते हैं वही अत्याचारी हैं (वह स्वयं अपने प्रति अत्याचार करते हैं) । '' (क़ुरआन-60:8-9)
इस्लामी यु़द्ध अथवा जिहाद को लेकर इस्लाम और क़ुरआन के प्रति हमारे देश में जितना द्वेषपूर्ण तथा भ्रमामक प्रचार किया गया है, वह कितना निर्मूल तथा भ्रष्ट प्रचार है, यह हमने पवित्र क़ुरआन द्वारा सिद्ध कर दिया है। हमें आशा है कि अब गै़र-मुस्लिम भाइयों को पुराना अथवा नवीन कोई दुष्प्रचार प्रभावित न करेगा। अनुचित न होगा यदि अन्त में इस विषय से सम्बन्धित हम दो घटनाओं की भी चर्चा कर दें।
रामनगर ही में हमारे एक सनातन धर्मी मित्र है। अंग्रेजी के बी0ए0, संस्कृति के उच्चकोटि के विद्वान, कई पुस्तकों के लेखक और पुराणों के अनुवादक, विचार के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघी। उन्होंने एक बार लखनऊ के मासिक ‘‘राष्ट्र-धर्म'' का इस्लाम विरोधी एक लेख पढ़कर हमें सुनाया। उसमें पवित्र क़ुरआन की यह आयत थी-
‘‘मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों के विरुद्ध विधर्मियों को अपना संरक्षक-मित्र न बनाएँ।'' (क़ुरआन)
इस आयत से हमारे मित्र की भावना को बड़ी चोट चहुँची थी। इसका अनुवाद सुनाकर उन्होंने पूछा-‘‘अनुवाद ठीक है?'' मैंने कहा - ‘‘अनुवाद तो ठीक है, परन्तु इसका वह उद्देश्य नहीं है जो लेखक ने बताया है। इस आयत का सम्बन्ध मक्का निवासियों से है जो मदीना पर आक्रमण कर रहे थे और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। जो मुसलमान मक्का त्याग करके मदीना चले आए थे, उनमें से कुछ के सम्बन्धी मक्का में रह गए थे। मदीना के ऐसे ही मुसलमानों के सम्बन्ध में यह आयत है।'' फिर मैंने अपने मित्र को मौलाना अबुल कलाम के तर्जुमानुल क़ुरआन से आयत का तात्पर्य पढ़कर सुनाया जो यह है-
‘‘चूंकि अब निर्णय का समय आ गया है, इसलिए इस्लाम के अनुयायियों को सम्बोधित करके कहा गया है कि वे कार्यरत हो जाएँ और दुर्बलता न दिखाएँ। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों को सामूहिक सम्बन्धों पर प्रधानता न दें तथा शत्रुओं को अपना सहायक और मित्र न बनाएँ।
युद्ध-क्षेत्र गर्म हो चुका है। मित्र और शत्रु की दो पंक्तियाँ अलग-अलग खड़ी हो गई हैं। अतः हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने लिए कोई एक पंक्ति का चुनाव कर ले और जिसे ग्रहण कर ले; उसका हो रहे। यह न हो कि एक का होकर दूसरे से भी गुप्त सम्बन्ध रखे।'' (भाग 1, पृष्ठ 318)
यह व्याख्या सुनाकर मैंने सूरा बक़रा की वे आयतें दिखाईं जिनको हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं। कहा- ‘‘वे आयतें देखिए जिनमें घोर युद्ध की शिक्षा दी गई है और आयतों के एक-एक वाक्य का आशय समझाया तो, मेरे मित्र जो स्वंय सेवक-संघी होने के साथ धार्मिक भावना के व्यक्ति है, वे इन आयतों के तात्पर्य से अवगत होकर इतने प्रभावित हुए कि जब मैं युद्ध सम्बन्धी और आयतें दिखाने चला तो रोक दिया-कहा हम समझ गए; वह विरोधियों से सम्बन्धित है।'
दूसरी घटना यह है कि मेरी यह पुस्तिका ‘ईमारते शरीआ बिहार और उड़ीसा' ने भी प्रकाशित की थी। नगर के जिन हिन्दू भाइयों से मारत का सम्बन्ध था उनको प्रकाशन से पहले यह पुस्तिका दिखाई गई। उन्होंने कहा-‘‘यह प्रकाशित कराई जाए, यह अपने विषय में सफल है।''
इन दोनों प्रयोगों से हमें विश्वास है कि न्यायशील और शुद्ध हृदय हिन्दू भाई इस पुस्तिका से उचित प्रभाव ग्रहण करेंगे।
धार्मिक स्वतन्त्रता
महाईश-दूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके उत्तराधिकारियों के समय में गै़र-मुस्लिम से बहुत-सी संधियाँ हुईं और उनके लिए प्रतिज्ञा-पत्र लिखे गए। हम उनके धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।
माह दीनदार के निवासियों को जो प्रतिज्ञा-पत्र लिखा गया उसमें था-
‘‘न उनका धर्म बदला जाएगा और न उनके धार्मिक कार्यों में हस्ताक्षेप किया जाएगा।''
जुर्जान निवासियों के प्रतिज्ञा-पत्र में था-
‘‘उन के प्राण, धन, धर्म, शास्त्र सबके लिए सुरक्षा है, उनकी किसी चीज़ में परिवर्तन न किया जाएगा।''
लूकाफ़ और आज़र बाईजान निवासियों के प्रतिज्ञा-पत्र में था-
‘‘ग़ैर-मुस्लिमों के प्राण, धन, धर्म और शास्त्र सबके लिए रक्षा है।''
ये पंक्तियाँ बड़े आलिम शिबली की पुस्तक ‘अलफ़ारूक़' से उद्धत की गई हैं।
हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) की उपस्थिति में ईलिया (शाम) के निवासियों को जो प्रतिज्ञा-पत्र लिखा गया उसमें है-
‘‘यह वह सुरक्षा है जो ईश्वर के दास और मुसलमानों के अधिकारी (ख़लीफ़ा) उमर ने ईलिया निवासियों को दी। यह सुरक्षा उनके प्राण, धन, उपासनागृह, सलीब, स्वास्थ्य, रोगी तथा उनके समस्त सहधर्मियों के लिए है। वह इस प्रकार है कि न उनके उपासनागृहों में निवास किया जाएगा, न उनको ढाया जाएगा, न उनके अहाते को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाएगी और न उनकी सलीबों और माल में कोई कमी की जाएगी और न उनके धर्म के सम्बन्ध में उन पर कोई दबाव डाला जाएगा।''? (अल-फ़ारूक़)
यह कुछ विशेष उदारता नहीं है। धार्मिक स्वतन्त्रता और धार्मिक रक्षा इस्लामी शासन की स्थायी नीति थी, जो पवित्र क़ुरआन के इस आदेश पर आधारित थी- ‘ला इकरा-ह फ़िद्दीन' (धर्म के विषय में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं) । हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) के शासनकाल में हज़रत अम्र बिन आस ने मिस्र को जीता। युद्ध में बहुत-से सैनिक बन्दी बने थे, मिस्र के विजेता हज़रत अम्र बिन आस ने हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) से लिखकर पूछा कि बन्दियों के सम्बन्ध में क्या किया जाए? हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) ने उत्तर में लिखा कि बन्दियों को इसका अधिकार दे दिया जाए कि वे चाहें तो इस्लाम ग्रहण कर लें और चाहें तो जिज़्या देना स्वीकार करके अपने धर्म पर रहें। (अल-फ़ारूक़-अल्लामा शिबली)
हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) का एक दास ईसाई था। एक बार उन्होंने दास से मुसलमान हो जाने का प्रस्ताव किया, उसने अस्वीकार कर दिया। हज़रत उमर (रज़िअल्लाहु अन्हु) का शासन, ईरान, शाम और मिस्र तक फैला हुआ था, परन्तु आपने उसका उत्तर सुनकर कहा-ला इकरा-ह फ़िद्दीन' (धर्म के विषय में ज़बरदस्ती नहीं)। इतना ही नहीं, आप उससे अप्रसन्न भी नहीं हुए। अपने इन्तिक़ाल के समय दास को गले लगाया और उसे स्वतन्त्र कर दिया।
शाम के अंताकिया नगर के याकूबी सम्प्रदाय का पीटर यार्क मीकाईल लिखता है-
‘‘जब ख़ुदा ने रोमनों का उत्पात देखा कि वे जहाँ कहीं अधिकार पाते हैं हमारे गिरजाओं को अशुद्ध कर देते हैं और हम पर अत्याचार करते हैं, तो उसने प्रदेश में इस्माईल की सन्तान (मुसलमानों) को नियुक्त किया कि वे हमें रोमनों से मुक्ति दिलाएँ।''
एक नस्तूरी उस्क़ुफ़ (धर्म-नेता) कहता है-
‘‘अरब मुसलमान, ईसाइयों के मज़हब से नहीं लड़ते, वे हमारे पादरियों और मज़हबी बुजुर्गों का सम्मान तथा हमारे मज़हब की रक्षा करते हैं, वे बड़े उदार है।''
महाईश दूत के तीसरे उत्तराधिकारी हज़रत उस्मान (रज़िअल्लाहु अन्हु) के शासन-काल में डीसुजा ने, जो मरू का पीटर यार्क था, ईरान के लार्ड बिशप साईमन को लिखा-
‘‘अरब, जिनको ख़ुदा ने इस समय देशों की बादशाहत दी है, ईसाई मज़हब पर आक्रमण नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत हमारे मज़हब की सहायता करते हैं और हमारे गिरजाओं और ख़ानक़ाहों को अनुदान देते हैं।'' (हुक़ूक़ुज़्ज़िम्मीयीन, शिब्ली)
डा0 ई0एफ़0 क्रासवेल इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक हैं। अपने एक लेख में लिखते हैं-
‘‘मानव-जाति का एक महत्वपूर्ण विभाग युद्ध भी है और जीवन के इस क्षेत्र में नैतिक आदर्श को स्थापित रखना कठिन हो जाता है। परन्तु इस्लाम ने मानव-जीवन के इस क्षेत्र में भी केवल उच्चकोटि की नैतिक शिक्षा ही उपस्थित नहीं की है, बल्कि व्यावहारिक रूप में भी मुसलमान इस आदर्श को अपने सामने रखते रहे हैं।
इस्लाम ने आक्रमणात्मक युद्ध की हर अवस्था को निषिद्ध ठहराया है और मुसलमानों को केवल प्रतिरक्षात्मक युद्ध की अनुमति दी है। परन्तु ऐसे युद्ध में भी नैतिकता एवं मानवता के सीमोल्लंघन से कठोरता के साथ मनाही कर दी है और केवल उन्हीं लोगों पर हथियार उठाने की अनुमति दी है, जो मुसलमानों से लड़ें और पराजित होने के बाद भी हथियार डालने से इनकार कर दें। इसी के साथ उसने जीविका सम्बन्धी सामग्री को नष्ट करने की भी सर्वथा मनाही कर दी है। युद्ध के विषय में संसार की कोई जाति नैतिकता का इतना ऊँचा आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकती जितना इस्लाम ने प्रस्तुत किया है। सारांश यह कि इस्लाम को जिस ओर से भी देखा जाए वह उच्चकोटि की नैतिक शिक्षा का संग्रह सिद्ध है। उसकी शिक्षा का सबसे बड़ा गुण यह है कि उससे मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम दोनों समान रूप से लाभान्वित हो सकते हैं।'' (मासिक ‘‘दीन-दुनिया'' दिल्ली, जून सन् 1960 ई0)
जिज़्या
जिहाद ही की तरह जिज़्या को लेकर भी इस्लाम के विरुद्ध बड़ा दुष्प्रचार किया गया है और यह ग़लतफ़हमी उत्पन्न कर दी गई है कि जिज़्या का उद्देश्य भी कर-भार द्वारा गै़र मुस्लिमों को इस्लाम ग्रहण करने पर बाध्य करना है। हर प्रकार के इस्लाम-विरोधी प्रचार का स्रोत तो ईसाई सम्प्रदाय है, परन्तु अंग्रेज़ों के शिष्य उनके चबाए ग्रास को चबानेवाले हमारे देश के विद्वानों ने भी जिहाद और जिज़्या के प्रति बड़ा द्वेषपूर्ण प्रचार किया है। उन्हीं विद्वानों मे अंग्रेजी सरकार के सेवक तथा सम्मानित मुग़ल इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार ‘सर यदुनाथ सरकार' भी थे।
उनकी एक हिन्दी पुस्तक ‘औरंगज़ेब' है। यद्यपि वह हिन्दी नहीं जानते थे, परन्तु उन्हीं की इच्छा के अनुसार उनके एक शिष्य ने उनकी अंग्रेज़ी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद कराके उनकी स्वीकृति के बाद उन्हीं के नाम से प्रकाशित कराया है। किसी धर्म के विषय में प्रमाण उसी धर्म की पुस्तकें हो सकती हैं, विरोधियों की लिखी हुई पुस्तकें नहीं हो सकतीं, चाहे वे कितने बड़े विद्वान हों। उदाहरणत: वेद-शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकें काशी, अयोध्या, मथुरा आदि के पंडितों ही की प्रमाण होंगी, न कि इंग्लैण्ड के विद्वानों की। यदुनाथ सरकार ने उक्त पुस्तक में इस्लाम के विषय में जो कुछ लिखा है उसका आधार इस्लामी पुस्तकें नहीं हैं, इस्लाम के शत्रु अंग्रेज़ों की ‘ह्यूज'और ‘इनसाईक्लोपीडिया आफ़ इस्लाम' आदि है, जिनका उद्देश्य इस्लाम के विरुद्ध भ्रम, घृणा, तथा द्वेष उत्पन्न करना था। इसलिए आवश्यकता है कि संक्षेप में जिज़्या की वास्तविकता भी गै़र मुस्लिम भाइयों के सामने पेश कर दी जाए।
पहले हम यह बता दें कि जिज़्या ग़ैर-मुस्लिमों ही पर क्यों है?
1-मुसलमानों पर एक धार्मिक अनिवार्य ‘कर' लागू होता है, जिसको ‘ज़कात' कहते हैं। इसकी दर ढाई प्रतिशत सालाना है, जो बचत के धन पर देना पड़ता है। यदि कोई अरबपति हो तो उसको भी ढाई प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष ज़कात देनी पड़ती है और यदि देश पर कोई संकट आ जाए तो इस्लामी शासन मुसलमानों से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार विशेष धन भी प्राप्त कर सकता है। परन्तु ग़ैर-मुस्लिम प्रजा से जिज़्या के अतिरिक्त एक पैसा नहीं ले सकता।
2.गै़र-मुस्लिम प्रजा देश की सुरक्षा के दायित्व से मुक्त होती है इसलिए सैनिक ख़र्च के लिए उससे हल्का-सा देश-सुरक्षा कर लिया जाता है; वही जिज़्या कहलाता है। आवश्यकता पड़ने पर जो ग़ैर-मुस्लिम प्रसन्नतापूर्वक सैनिक सेवा में भाग लेते हैं उनसे जिज़्या नहीं लिया जाता। यदुनाथ सरकार ने इस विषय में जो कुछ लिखा है वह मिथ्या है।
3-इस्लामी राज्य की तमाम गै़र-मुस्लिम प्रजा पर जिज़्या अनिवार्य नहीं है। इस्लामी राज्य की गै़र-मुस्लिम प्रजा तीन प्रकार की होती है। एक वे गै़र-मुस्लिम जिन्होंने किसी प्रकार की संधि के द्वारा इस्लामी राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली हो। उनके साथ इस्लामी शासन संधि की शर्तों के अनुसार व्यवहार करता है। यदि संधि में जिज़्या की शर्त न हो तो इस्लामी शासन को उन पर कदापि जिज़्या लगाने का अधिकार नहीं है। दूसरी क़िस्म उन गै़र-मुस्लिमों की है, जिन्होंने इस्लामी राज्य से युद्ध किया हो और युद्ध करते हुए पराजित हो गए हों तथा इस्लामी सेना ने उनके नगर और दुर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया हो। केवल यही ग़ैर-मुस्लिम है, जिनके लिए नियम है कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनके सब अधिकार इस्लामी समाज के बराबर हो जाते हैं और अपने धर्म पर रहना चाहें तो ‘सुरक्षाकर' के रूप में उन पर जिज़्या लगाया जाता है। तीसरे वे गै़र-मुस्लिम हैं जो न दोनों प्रकार के अतिरिक्त किसी और प्रकार से इस्लामी राज्य के नागरिक बन गए हों । उदाहरणस्वरूप पाकिस्तान के गै़र-मुस्लिम, उन पर किसी प्रकार से भी जिज़्या नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि वे न युद्ध में पराजित हुए हैं और न जिज़्या स्वीकार करके पाकिस्तान की प्रजा बने हैं। वह मूलतः पाकिस्तान के नागरिक हैं।
इस्लामी परिभाषा में तीनों प्रकार की गै़र-मुस्लिम जनता ‘ज़िम्मी' कहलाती है। ज़िम्मी कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इसका अर्थ है वे गै़र-मुस्लिम जिनके प्राण, धन, धर्म, सम्मान, सुख, शान्ति, सबकी संरक्षा का इस्लामी शासन ज़िम्मेदार होता है। इतना ही नहीं व्यावहारिक रूप से गै़र-मुस्लिमों की हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व इस्लामी शासन पर होता है, परन्तु इस्लाम के अनुसार ग़ैर-मुस्लिमों की रक्षा के वास्तविक ज़िम्मेदार अल्लाह और रसूल होते हैं। ईश्वर दूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया है-
‘ख़बरदार! जो कोई गै़र-मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार करेगा या उसके अधिकार में कमी करेगा अथवा उस पर उसकी शक्ति से अधिक किसी प्रकार का भार डालेगा या उसकी प्रसन्नता के बिना उसकी कोई वस्तु लेगा तो क़ियामत के दिन उसके विरुद्ध उस ग़ैर-मुस्लिम प्रजा की ओर से खु़दा के सम्मुख मैं वादी बनूँगा।''
ग़ैर-मुस्लिम भाई गम्भीरतापूर्वक महाईश-दूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इस चेतावनी पर विचार करें जो उन्होंने मुसलमानों को दी है। सुरक्षा की ऐसी गारन्टी तो हम भारतीय जनता को भी प्राप्त नहीं है। साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमानों के साथ क्या होता है ?
4-जिज़्या की दर इस प्रकार है- धनवान पर चाहे वह लखपति और अरबपति ही क्यों न हो हर व्यक्ति प्रति वर्ष 12 रू0 मध्यम वर्ग पर 6 रू0 व्यापारी और नौकरी पैशा वर्ग पर 3 रू सालाना। जिज़्या के प्रति मूल सिद्वान्त यह है कि इतने ही धन के अनुसान जिज़्या लिया जाए जो आवश्यकता से अधिक हो। यदि किसी ग़ैर-मुस्लिम प्रजा की आय कम हो जाए तो उससे तीन रूपया से भी कम लिया जाएगा, परन्तु आय बढ़ जाने पर जिज़्या बढ़ाया नहीं जा सकता।
5-जिन पर जिज़्या लागू होता है, उनमें भी स्त्रियाँ, बालक, पागल, अन्धे, अपाहिज, मन्दिरों और पूजागृहों के सेवक, साधु-समाज, गृहस्थ, जीवन से अलग होकर गुफाओं और मठों में रहनेवाले लोग जिज़्या से मुक्त होते हैं।
6- जिज़्या देने के लिए अधिकारियों के पास जाने का नियम नहीं है। अधिकारियों को स्वयं वुसूली के लिए जाना पड़ता है। इनको आदेश है कि जिज़्या की वुसूली में नम्रता से काम लें। कठोरता का व्यवहार न करें। उनके वस्त्र इत्यादि आवश्यकता की वस्तुएँ नीलाम न करें।
7-धनहीनों और भिक्षा माँगनेवाले गै़र-मुस्लिमों का सरकारी कोष में भी अधिकार है। यदुनाथ सरकार की ‘औरंगज़ेब' पुस्तक में इन नियमों की कोई चर्चा नहीं है। यदि जिज़्या गै़र-मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए होता तो मन्दिरों के पुजारी, साधु, संन्यासी, मठों और गुफाओं में रहनेवाले तथा स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े और धनहीन जिज़्या से मुक्त न होते।
यह बात तो हम इसी पुस्तिका में ऊपर लिख चुके हैं कि इस्लामी राज्य में ग़ैर-मुस्लिम प्रजा को प्राण, धन, धर्म, सम्मान सबकी पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है।यहाँ हम इतना और बता दें कि इस्लामी विधान मनुष्यों के बनाए हुए विधान के अनुसार नहीं होता, ईश्वरीय ग्रन्थ क़ुरआन और महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के आदेशों पर आधारित होता है। अतः उसकी अवहेलना उसी प्रकार पाप है जिस प्रकार दूसरी ईश्वरीय आज्ञाओं तथा महाईश्दूत के आदेशों की अवज्ञा पाप है।
वास्तविकता के विरुद्ध कितना ही प्रचार किया जाए वह अपनी वास्तविकता मनवाकर ही रहती है। पश्चिम के विद्वानों ही में ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने दुराग्रह के दुष्प्रचारों का खण्डन किया। सर यदुनाथ सरकार जैसे विद्वानों को अंग्रेज़ों की राजनीति के अनुसार इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध दुष्प्रचार करना था, वे ऐसे विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन क्यों नहीं करते जिन्होंने दुष्प्रचार का खण्डन किया है ? मान्य पाठक देखें-
मिस्टर हालम अपने इतिहास ‘‘अंग्रेज़ी साम्राज्य विधान,'' प्रथम भाग, अध्याय-2 में लिखते हैं-
‘‘इस्लाम धर्म लोगों के सामने उपस्थित किया गया, परन्तु उनसे कभी अनिच्छापूर्वक ग्रहण नहीं कराया गया और जिस व्यक्ति ने इस धर्म को प्रसन्न हृदय से स्वीकार कर लिया, उसको वही अधिकार प्रदान किए गए जो विजयी जाति के थे। इस धर्म ने विजित जातियों को उन शर्तों से मुक्त कर दिया जो संसार के आरम्भ से इस्लाम के पैग़म्बर के समय तक हर विजयी ने विजितों पर लागू की थीं। इस्लामी नियम के अनुसार अन्य धर्मवालों को जो इस्लामी राज्य के अधीन और आज्ञाकारी थे, हर प्रकार की धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई जो इस दावे पर कि (दीन में ज़बरदस्ती नहीं) एक खुला हुआ प्रमाण और एक अकाट्य तर्क है। इस्लाम में अन्य धर्मवालों को धार्मिक स्वतन्त्रा देने और उनके साथ सद्व्यवहार करने की आज्ञा से सम्बन्धित यह आयत किसी पागल की बकवास नहीं है न किसी दार्शनिक का निराधार विचार है, बल्कि यह उस व्यक्ति का कथन है जो ऐसे साम्राज्य का शासक था जो इतनी शक्ति रखता था और जिसकी व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि वह जैसा नियम चाहता, जारी कर सकता था। (उपर्युक्त वाक्य ईश्वर प्रदत्त क़ुरआन का है-लेखक) धर्म में भी और सांस्कृतिक राजनीति में भी अनेक व्यक्तियों और सम्प्रदायों ने धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का प्रलोभन दिया है, मगर इसके कार्यान्वित करने की ताकीद सिर्फ़ उस समय तक है जब तक वह विवश और निर्बल रहे हैं। लेकिन इस्लाम के पैग़म्बर ने धार्मिक स्वतन्त्रता देने का प्रलोभन ही नहीं दिया, बल्कि उसको धार्मिक नियमों में सम्मिलित कर दिया। हर जाति जो मुसलमानों के राज्य और अधिकार में आई उसके साथ दया और प्रेम करने का सिद्धान्त प्रयुक्त किया गया और हर जाति से उसके अपने धार्मिक संस्कार और कार्य किसी रोक-टोक के बिना करते रहने का पारिश्रमिक नाम-मात्र कर के रूप में लिया गया । और जब एक कर निश्चित हो जाता है तो फिर उस जाति की धार्मिक मान्यताओं और कार्यो में हस्तक्षेप करना सर्वथा धर्म-विरुद्ध और निषिद्ध समझा जाता था।'' प्रसिद्ध फ़्रांसीसी विद्वान डॉक्टर लीबान लिखता है-
‘‘हम जिस समय अरबों की विजय पर दृष्टि डालेंगे और उनकी सफलता के कारणों को उजागर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि धर्म के प्रचार में तलवार से कुछ भी काम नहीं लिया गया, क्योंकि मुसलमान सर्वदा विजित जातियों को अपने धर्म के पालन में स्वतन्त्र छोड़ देते थे। यदि ईसाई जातियों ने अपने विजेताओं के धर्म को स्वीकार कर लिया और अन्त में उनकी भाषा भी ग्रहण कर ली तो यह केवल इस कारण से था कि उन्होंने अपने नए शासकों को अपने पुराने शासकों से अधिक सत्य और सरल पाया।''
दूसरे स्थान पर यही इतिहासकार लिखता है-
‘‘मुसलमान ख़लीफ़ाओं ने मुल्की उद्देश्य से कदापि तलवार द्वारा धर्म फैलाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि जैसाकि बार-बार कहा जाता है कि वह बलपूर्वक अपने धर्म का प्रचार करते थे इसके विपरीत वे पूरी तरह स्पष्ट कर देते कि विजित जातियों के धर्मों, संस्कारों और वेश-भूषा का पूरा सम्मान किया जाएगा और इस स्वतन्त्रता के बदले वे उनसे एक हल्का-सा कर (जिज़्या) लेते थे, जो उन करों की अपेक्षा जो उन जातियों के भूतपूर्व शासक करते थे, बहुत-ही कम था।''
एक और स्थान पर डॉक्टर लीबान ने लिखा है-
‘‘अरबों के शासन में ईसाइयों को धर्म, रीति-रिवाज और नियम की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। एक राहिब (ईसई संन्यासी) जिसका नाम करादीन था और जो पलरमों के गिरजा सेंट कैथरीन का पादरी था, लिखता है कि पादरियों को इस बात की पूर्ण स्वाधीनता थी कि वे अपने धार्मिक वस्त्र पहनकर रोगियों को तसल्ली देने जाया करें। एक दूसरा पादरी मोरकोली वर्णन करता हें कि सेना में समस्त धार्मिक संस्कारों में दो धार्मिक झण्डे खड़े होते थे, एक झण्डा मुसलमानों का जो हरे रंग का होता था और उसपर काला बुर्ज बना रहता था और दूसरा ईसाइयों का जो लाल रंग का होता था और उस पर सुनहरी सलीब बनी रहती थी। मुसलमानों की विजय के समय जितने गिरजे थे सब स्थापित रखे गए।''
यही इतिहासकार दूसरी जगह पर लिखता है-
‘अरब शासनकाल में अधिकता के साथ गिरजों का निर्माण होना भी इस बात का प्रमाण है कि वे विजित जातियों के धर्म का कितना सम्मान करते थे।
बहुत-से ईसाई मुसलमान हो गए, लेकिन इस्लाम ग्रहण करने की कुछ ऐसी आवश्यकता न थी, क्योंकि अरबों के शासन में ईसाई भी जिनको मुस्तअरब कहते थे एवं यहूदी हर प्रकार से मुसलमानों के बराबर थे और उन्हें भी शासन के पद मिल सकते थे। ''
इन दोनों विद्वानों के जो उद्धरण पेश किए है उनसे सर यदुनाथ सरकार द्वारा किए गए दुष्प्रचार का पूरी तरह खण्डन हो जाता है।
अब एक भारतीय विद्वान की समीक्षा देखिए-डॉक्टर ईश्वर टोपा, एम0ए0, डी0लिट, लिखते हैं-
‘‘जिज़्या लगाने और मन्दिरों को तोड़ने की घटनाओं से जो मिथ्या परिणाम निकाले जाते हैं उन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जिज़्या हिन्दू जनता को आर्थिक दासता में फँसाने के लिए लगाया गया था। इन दावों की विद्वतापूर्ण समीक्षा की आवश्यकता है।
इस्लामी शास्त्र की परिभाषा में ग़ैर-मुस्लिम केवल एक साधारण-सा ‘कर' देकर, जो जिज़्या कहलाता है, इस्लामी राज्य की सुरक्षा में आ जाते हैं। हर मुसलमान को सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है परन्तु गै़र-मुस्लिम जिज़्या देकर सैनिक सेवा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ज़िम्मियों के प्राण, धन और उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता अर्थात् उनकी रीति-रिवाज के अनुसार पूजागृहों में पूजा-पाठ का इस्लामी राज्यसंरक्षक होता है। इस्लामी राज्य अपने नियम से बंधा हुआ होता है और इस्लामी नियम उसे ज़िम्मियों के धार्मिक कृत्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देता। फिर वह मन्दिरों को कैसे तोड़ सकता है? जब ज़िम्मी अपने दायित्व को पूरा कर देता है तो इस्लामी राज्य पर स्वयं इसका दायित्व लागू हो जाता है। इस्लाम धर्म में जिज़्या का यही सिद्धान्त है।
इस्लामी राज्य का एक उज्ज़वल पक्ष और है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । जिज़्या सब ग़ैर-मुस्लिमों पर नहीं लगाया जाता, अधिकार लोग इससे मुक्त होते हैं। स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों, पुजारियों, विद्यार्थियों, बेरोज़गारों, निर्धनों और भिखारियों को जिज़्या नहीं देना पड़ता। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि कम से कम 75 प्रतिशत गै़र-मुस्लिम जिज़्या से मुक्त होते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे ही व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। ''
आगे चलकर विद्वान लेखक ने बताया है कि भारत का आरम्भिक मुस्लिम राज्य इस्लामी राजनीति का आदर्श था। उसने ग़ैर-मुस्लिमों के साथ, न्यायपूर्ण ही नहीं उदारतापूर्ण व्यवहार भी किया जिससे प्रसन्न होकर स्वयं ग़ैर-मुस्लिमों ने उनके शासन की जड़ सुदृढ़ की और उनके बाद जो मुसलमान शासक हुए उनका शासन वास्तविक इस्लामी शासन न था, इसलिए उनके शासन का दोष इस्लाम पर नहीं आता। (मासिक नई ज़िन्दगी, अक्टूबर सन् 1946 ई0 इलाहाबाद)
ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा प्रयास सफल हो, जिहाद और जिज़्या विषयक भ्रम का निवारण हो जाए।
----------------------------
Follow Us:
E-Mail us to Subscribe E-Newsletter:
HindiIslamMail@gmail.com
Subscribe Our You Tube Channel
Recent posts
-

रमज़ान तब्दीली और इन्क़िलाब का महीना
20 June 2024 -
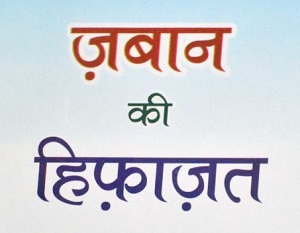
ज़बान की हिफ़ाज़त
15 June 2024 -
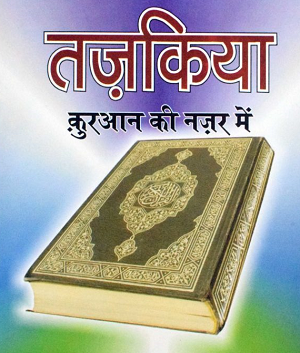
तज़किया क़ुरआन की नज़र में
13 June 2024 -

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (ख़ुतबात मुकम्मल)
27 March 2024 -

रिसालत
21 March 2024 -

इस्लाम के बारे में शंकाएँ
19 March 2024

