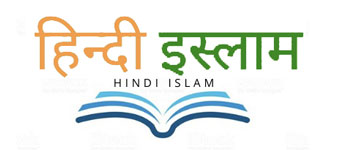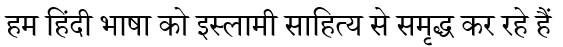फ़िक़्हे-इस्लामी आधुनिक काल में (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 12)
-
फ़िक़्ह
- at 17 April 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक: गुलज़ार सहराई
लेक्चर नम्बर-12 (27 September 2004)
फ़िक़्हे-इस्लामी की नई समझ की ज़रूरत
आज की चर्चा का शीर्षक है ‘फ़िक़्हे-इस्लामी आधुनिक काल में’। आधुनिक काल में फ़िक़्हे-इस्लामी का अध्ययन और उसको लागू करना एक ऐसा विषय है जो एक दृष्टि से अतीत की चर्चाओं को निरन्तर आगे बढ़ाता है और एक-दूसरी दृष्टि से मुसलमानों के भविष्य का पहला अध्याय या पहला क़दम है। अगर मुस्लिम जगत् का भविष्य सुखद है, अगर मुस्लिम जगत् के आगामी जीवन का नक़्शा उनकी अपनी अभिलाषाओं और तमन्नाओं की रौशनी में गठित होना है, अगर मुस्लिम देशों का आगामी राजनैतिक जीवन आत्मनिर्भर, आज़ाद और सम्माननीय भविष्य पर आधारित है, और निश्चय ही ऐसा ही है तो ऐसा केवल और केवल एक आधार पर सम्भव है। वह यह कि मुसलमान इस्लामी शरीअत के बारे में अपने आम रवैये पर पुनर्विचार करें। आधुनिक काल में फ़िक़्हे-इस्लामी की समझ नए सिरे से प्राप्त करें और इस भूले हुए रिश्ते को खोज निकालें जिससे उनका सम्बन्ध पिछले कई सौ वर्षों से या तो टूट गया है या कमज़ोर पड़ गया है।
आधुनिक काल में मुस्लिम जगत् के मुसलमान या तो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, या अपनी दीनी (धार्मिक) और इस्लामी पहचान की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, और या विभिन्न ग़ैर-इस्लामी, पश्चिमी और पूर्वी धारणाओं के वर्चस्व के ख़िलाफ़ मुस्लिम जगत् के मूल विचारों एवं विचारधाराओं के पुनरुत्थान के लिए प्रयासरत हैं।
इस सारी स्थिति में जो चीज़ उनकी जीवनियों को नया गठन प्रदान कर सकती है वह फ़िक़्हे-इस्लामी की नई समझ है। फ़िक़्हे-इस्लामी की नई समझ से हरगिज़ यह नहीं समझना चाहिए कि नई समझ अतीत की समझ से भिन्न होगी, या इस्लाम के बड़े फ़ुक़हा की समझ एवं अन्तर्दृष्टि पर अविश्वास का द्योतक होगी। बिलकुल नहीं, बल्कि यह समझ अतीत की समझ ही का क्रम होगा। यह समझ इस्लाम के दौर के अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन (चार बड़े इमामों) की समझ का क्रम और पुनरुत्थान होगा। जिस अंदाज़ से इस्लाम के आरम्भिक चार पाँच सौ वर्षों में फ़िक़्हे-इस्लामी ने उनका मार्गदर्शन किया, उसी अंदाज़ का मार्गदर्शन फ़िक़्हे-इस्लामी मुसलमानों के भविष्य के लिए कर सकती है और इंशाअल्लाह करेगी।
इस सन्दर्भ में आज जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे दो हैं। पहली चीज़ तो यह है कि पिछले तीन-चार सौ वर्षों के पतन के दौर में जहाँ मुसलमानों में और बहुत-सी कमज़ोरियाँ पैदा हुईं, वहाँ फ़िक़्ह के बारे में उनके रवैये में एक जड़ता और एक ठहराव की-सी कैफ़ियत सामने आई। इस जड़ता और ठहराव के कारण क्या थे, इसपर एक लम्बी चर्चा की जा सकती है जो आज के विषय से बाहर है। लेकिन यह एक वास्तविकता और सच्चाई है कि पिछले तीन सौ वर्षों के दौरान जिस तरह मुसलमानों के जीवन के दूसरे विभागों में एक जड़ता और पतन हुआ है इसी तरह फ़िक़्हे-इस्लामी में उनकी समझ और फ़िक़्हे-इस्लामी के बारे में उनके रवैये में भी जड़ता और पतन ने जगह पाई। इस दौर में फ़िक़्हे-इस्लामी के विषयों के बारे में उनका शोध, लेखन कार्य, फ़तवों का ज्ञान, शिक्षा ग़रज़ हर चीज़ के बारे में यह जड़ता एवं पतन बीसवीं सदी के मध्य तक बढ़ता हुआ और फैलता हुआ महसूस होता था। बीसवीं सदी का मध्य विशेषकर और बीसवीं सदी का आरम्भ आम तौर से फ़िक़्हे-इस्लामी में एक नए जीवन और नए दौर का आरम्भ है।
आज की चर्चा में फ़िक़्हे-इस्लामी के इस नए दौर का अध्ययन करना अभीष्ट है। इसमें यह देखने की कोशिश भी की जाएगी कि जब बीसवीं सदी का आरम्भ हुआ तो फ़िक़्हे-इस्लामी कहाँ खड़ी थी। फ़िक़्ह के क़ाफ़िले की गाड़ी किस मरहले पर और किस प्लेटफ़ार्म पर खड़ी थी। बीसवीं शताब्दी में क्या परिवर्तन हुए। आज मुसलमान किन परिस्थितियों से दो-चार हैं और भविष्य में फ़िक़्हे-इस्लामी के बारे में उनका रवैया क्या होना चाहिए।
फ़िक़्हे-इस्लामी बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में फ़िक़्हे-इस्लामी के इतिहास में दो बड़ी घटनाएँ घटित हुईं। एक बड़ी घटना जो बहुत महत्त्वपूर्ण थी वह यह थी कि उन्नीसवीं सदी का लगभग पूरा समय मुसलमानों और विभिन्न पश्चिमी ताक़तों के दरमियान पहली बार सीधा टकराव पैदा हुआ। यह सारा दौर मुस्लिम जगत् और पश्चिमी जगत् के दरमियान एक बहुआयामी टकराव का ज़माना है। विभिन्न पश्चिमी ताक़तों ने मुस्लिम जगत् पर क़ब्ज़ा किया। मुस्लिम जगत् की सबसे बड़ी शक्ति सल्तनते-उस्मानिया के प्रत्यक्ष सम्पर्क पश्चिमी देशों से विस्तृत पैमाने पर शुरू हुए जिनकी हैसियत अब बराबर के दो पक्षों के बीच सम्पर्कों की नहीं रही थी, बल्कि अब एक कमज़ोर और पतन की ओर अग्रसर पक्ष का मामला एक शक्तिशाली, प्रभावशाली और दिन-प्रतिदिन सशक्त होते पक्ष से था। व्यापार, राजनियक मामले, जंग और सुलह, अनुबन्ध और इस तरह के बहुत-से नए-नए सम्बन्ध उस्मानी साम्राज्य और पश्चिमी शक्तियों के दरमियान सामने आने लगे। उस्मानी साम्राज्य की दिन-प्रतिदिन राजनैतिक और सैन्य कमज़ोरी, पश्चिमी शक्तियों की ताक़त और वर्चस्व, उस्मानी साम्राज्य की तंगहाली और पश्चिमी ताक़तों के संसाधन और बेपरवाही, इन सब चीज़ों ने मिलकर कुछ ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जिनके बारे में मुसलमानों ने इससे पहले ग़ौर नहीं किया था। उनके फ़िक़ही संग्रह में बहुत-सी ऐसी नई समस्याओं का जवाब नहीं था जो अब इन नई परिस्थितियों में पैदा हो रहे थे। यह कमज़ोरी या नासमझी फ़िक़्हे-इस्लामी की नहीं, मुसलमानों के अपने ज़ेहन और हौसले की थी। फ़िक़्हे-इस्लामी के बड़ों ने जब फ़िक़्ह के सर्वप्रथम संग्रह को संकलित किया तो वह मुसलमानों के उत्थान और प्रतिष्ठा का दौर था। आज़ादी, प्रतिष्ठा और उत्थान का मनोविज्ञान ही और होता है। वह नेतृत्व करनेवालों और विजेताओं की फ़िक़्ह थी। अब ज़माना पराजित और अनुकरण करनेवालों का था। वे इज्तिहादात स्वतंत्र चिन्तन करनेवालों के थे। अब ज़माना ग़ुलामों का था। गु़लामी का मनोविज्ञान भी और होता है। चरित्र के धनी लोगों का आसन अब बातें बनानेवालों के हाथ में था। पवित्र क़ुरआन के जिन स्पष्ट आदेशों से मिल्लत के आज़ाद लोग इज़्ज़त एवं गौरव का सन्देश पाते थे अब उम्मत के ग़ुलाम ज़ेहन उन्हीं आयतों से पिछड़ेपन और पतन का सन्देश निकाल रहे थे।
जब उस्मानी साम्राज्य का व्यापार बड़े पैमाने पर पश्चिमी ताक़तों विशेषकर फ़्रांस, यूरेशिया और हंगरी के साथ शुरू हुआ तो इस व्यापार के परिणामस्वरूप बहुत-सी ऐसी समस्याएँ सामने आईं जो इससे पहले मुसलमानों में पैदा नहीं हुई थीं और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने उनपर ग़ौर नहीं किया था। उनमें से एक महत्त्वपूर्ण समस्या इंशोरेंस और सेक्योरिटी की थी। उस ज़माने में इंशोरेंस को सेक्योरिटी कहा जाता था जिसके लिए अरबी भाषा की शब्दावली ‘सूकरह’ आम हुई। जो अंग्रेज़ी शब्द सेक्योरिटी का अरबी रूप था।
उन्नीसवीं सदी के अन्त के इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के यहाँ यह सवाल पैदा हुआ कि ‘सूकरह’ के नाम से जो रिवाज पश्चिमी दुनिया में प्रचलित है यह शरई रूप से जायज़ है कि नाजायज़ है। अगर जायज़ है तो उसके आदेश और सीमाएँ क्या हैं? और अगर नाजायज़ है तो उसके कारण क्या हैं। और अगर मुसलमानों से यह माँग की जाए कि वे इस कार्य-प्रणाली को बिलकुल छोड़ दें तो उसके विकल्प के रूप में क्या कार्य-नीति अपनाएँ। यह और इस तरह की बहुत-सी समस्याएँ उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में मुसलमानों के सामने आनी शुरू हुईं।
फिर चूँकि मुसलमान व्यापारी पश्चिमी दुनिया में बड़ी अधिकता से सामान लाने और ले जाने लगे और पश्चिमी दुनिया के व्यापारिक क़ाफ़िले भी मुस्लिम जगत् में बड़े पैमाने पर आने लगे। उनकी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ भी बड़े पैमाने पर माल लेकर आनी शुरू हुईं। इसलिए इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इस्लाम के व्यापार-क़ानून को ख़ास तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आदेशों को इस तरह से संकलित किया जाए कि पैदा होनेवाली समस्याओं के बारे में एक मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिम दोनों को यह मालूम हो कि उनके अधिकार और कर्त्तव्य क्या हैं।
फ़िक़्हे-इस्लामी का संकलन और नियम बनाना
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक फ़िक़्हे-इस्लामी एक असंकलित क़ानून था, जिसका मैं विस्तार से उल्लेख कर चुका हूँ। उसकी हैसियत इंग्लैंड के कॉमन लॉ की-सी थी। जो बाक़ायदा धाराओं के रूप में संकलित नहीं था। कॉमन लॉ भी संकलित क़ानून नहीं था, बल्कि बहुत-सी किताबों में, बहुत-सी चर्चाओं और विचारधाराओं के रूप में बिखरा हुआ था और अदालत का काम यह होता था कि जब कोई मुक़द्दमा सामने आए तो उन किताबों में तलाश करके इस बात का निर्धारण करे कि किसी स्थिति के लिए सम्बन्धित क़ानून कौन-सा है और जिस क़ानून को वह सम्बन्धित क़ानून क़रार दे उसके अनुसार उस मुक़द्दमे का फ़ैसला कर दे।
यही कैफ़ियत फ़िक़्हे-इस्लामी की थी कि फ़िक़्ह की वे किताबें, जिनमें कुछ का कल मैंने उल्लेख किया है, वे और इस तरह की हज़ारों किताबें पुस्तकालयों में मौजूद थीं। क़ाज़ी (जज) लोग इन किताबों से लाभान्वित होकर यह तय करते थे कि यह फ़तवा या यह क़ौल (कथन) या यह इज्तिहाद यहाँ इस स्थिति में सम्बन्धित और relevant है और इस मामले में उसको चरितार्थ किया जाना चाहिए। उसके आधार पर वे मुक़द्दमों का फ़ैसला कर दिया करते थे। इन इज्तिहादात या इन फ़तवों का शासकों या हुकूमतों से कोई सम्बन्ध नहीं था। ये सारी सामग्री और यह सारा क़ानूनी संग्रह एक आज़ाद ज्ञानपरक गतिविधि के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आ रहा था। ये सारी बहसें फ़ुक़हा अपने तौर पर किताबों के रूप में लिख रहे थे। गोया उस समय तक क़ानून का हर विभाग, क़ानून की हर धारा और क़ानून का हर आदेश शासकों के प्रभाव एवं पहुँच से पूरे तौर पर आज़ाद और उनकी अधिकार सीमा से बाहर था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे पश्चिम के लोग परिचित नहीं थे। उनके व्यापारी यह जानना चाहते थे कि जिस क़ौम और देश के लोगों से वे व्यापार कर रहे हैं उसके यहाँ व्यापार के आदेश क्या हैं। इसकी वजह से इस बात की आवश्यकता पेश आई कि यह क़ानून जो हज़ारों किताबों में बिखरे हुए हैं जिनसे न हर व्यक्ति परिचित हो सकता है और न ही हर व्यक्ति इस विस्तृत संग्रह का माहिर हो सकता है। लोगों की आवश्यकता की ख़ातिर उसको एक अलग किताब के रूप में संकलित किया जाए। ख़ास तौर पर मुसलमान व्यापारियों और उनसे मामला करनेवाले ग़ैर-मुस्लिम व्यापारियों को इसकी आवश्यकता रोज़ पेश आती थी।
मान लें, आप उस ज़माने में व्यापार कर रहे होते, और आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कोई कारोबार जर्मनी या फ़्रांस के किसी व्यापारी से हो रहा होता। कारोबार का आरम्भ करने से पहले वह व्यापारी यह जानना चाहता कि आपके देश में व्यापार के क़ानून और आदेश क्या हैं। अगर आपने मेरी बाक़ी रक़म अदा न की तो मैं आपके देश की किसी अदालत में कैसे और किस क़ानून के आधार पर अपना अधिकार वुसूल कर सकता हूँ। मुझे यह बताया जाए कि मेरे अधिकार क्या हैं। अब आपके लिए यह कहना तो बड़ा मुश्किल था कि तुम्हारे अधिकार एवं कर्त्तव्य फ़िक़्ह की संकलित किताबों में बयान हुए हैं। तुम फ़िक़्हे-हनफ़ी की किताबों में जाकर देख लो। ज़ाहिर है कि कोई पश्चिमी व्यापारी इस तरह अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्धारण नहीं कर सकता था। आपको दो-टूक अंदाज़ में बताना था कि यह क़ानून है जिसके आधार पर हमारे अधिकार और कर्त्तव्य निर्धारित होंगे।
‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ का संकलन
इस तरह के कारणों के आधार पर उस्मानी साम्राज्य में यह तय किया गया कि फ़िक़्हे-इस्लामी जो अब तक असंकलित और अलिखित संग्रह के तौर पर चला आ रहा है, उसको अब एक संकलित और संगठित क़ानून के तौर पर तैयार किया जाए। चुनाँचे उस्मानी साम्राज्य में विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई जिसमें साम्राज्य की सलाहकार समिति के सदस्य कुछ जज लोग और अल्लामा इब्ने-आबिदीन शामी, जिनका उल्लेख कल मैंने किया था, जो मुताख़्ख़िरीन में सबसे बड़े हनफ़ी आलिम थे, उनके पुत्र अल्लामा इब्ने-इब्ने-आबिदीन भी साझेदार थे। इस सात सदस्यीय कमेटी को यह बताया गया कि फ़िक़्हे-हनफ़ी की वे समस्याएँ जिनका सम्बन्ध व्यापार और कारोबार से है और व्यापारिक और कारोबारी लेन-देन के परिणामस्वरूप जो मुक़द्दमात पैदा होते हैं उनसे सम्बन्धित आदेशों को इस तरह से धारा अनुसार संकलित किया जाए कि इस धारा अनुसार संग्रह को एक क़ानून के रूप में लागू किया जा सके। चुनाँचे इस कमेटी ने इस काम का आरम्भ किया और लगभग बीस वर्ष इस काम में लगाए।
बज़ाहिर तो यह बड़ा आसान काम था। फ़िक़्हे-हनफ़ी की किताबें मौजूद थीं। उसमें से नक़्ल करके पंद्रह दिन में यह काम हो जाना चाहिए था, लेकिन यह काम इतना सादा और आसान नहीं था जैसा बज़ाहिर नज़र आता है। यह एक इज्तिहादी अंदाज़ का काम था। इसमें एक तो यह तलाश करना था कि फ़िक़्हे-इस्लामी और विशेषकर फ़िक़्हे-हनफ़ी में इन बड़ी-बड़ी समस्याओं से सम्बन्धित आदेश कौन से हैं जो आज व्यापारियों और कारोबारी वर्ग को आए दिन पेश आ रही हैं। फिर कुछ मामले जिनमें एक से अधिक रायें पाई जाती थीं, उनमें आजकल के हिसाब से सबसे सही और सबसे उचित राय कौन-सी है जो तर्कों के अनुसार भी मज़बूत हो। फिर कुछ ऐसी नई समस्याएँ भी थीं जिनके लिए नए आदेश दरकार थे, उन नए आदेशों को कैसे और किन सिद्धान्तों के आधार पर संकलित किया जाए। यह सब काम इस कमेटी ने बीस वर्ष की अवधि में किया। इसका आरम्भ 1856 ई॰ में हुआ। लगभग 1876 ई॰ में यह काम पूरा हो गया। जब यह काम पूरा हो गया तो इसकी शक्ल यह थी कि इस कमेटी ने सोला क़ानूनों पर आधारित आदेश तैयार किए। इन सब आदेशों को एक किताब के रूप में संकलित कर दिया गया। और शुरू में एक आरम्भिक अध्याय की वृद्धि कर दी गई जिसमें फ़िक़्हे-इस्लामी के कुछ मौलिक सिद्धान्त भूमिका और प्राक्कथन के रूप में बयान किए गए। इस तरह इस्लाम के इतिहास में पहली बार एक संकलित क़ानून और कोडिफ़ाइड लॉ संकलित हुआ जिसको ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ कहते हैं। यह उस्मानी साम्राज्य का पहला संकलित और कोडिफ़ाइड सिवल लॉ था जो फ़िक़्हे-इस्लामी से आम तौर पर और फ़िक़्हे-हनफ़ी से विशेषकर उद्धृत था। कहीं-कहीं इसमें फ़िक़्हे-हनफ़ी से हटकर दूसरे फ़ुक़हा के अक़्वाल (कथन) भी लिए गए थे। जब बीसवीं सदी का आरम्भ हुआ तो ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ पूरे उस्मानी साम्राज्य में लागू था। इस ज़माने में उस्मानी साम्राज्य की सीमाएँ पूर्वी यूरोप के कई देशों, तुर्की, मध्य एशिया का कुछ हिस्सा, इराक़, शाम, फ़िलस्तीन, लेबनान, अल-जज़ाइर, लीबिया, त्यूनीशिया और अरब द्वीप के कुछ इलाक़ों तक फैली हुई थीं। मिस्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस्मानी साम्राज्य के राजनैतिक और प्रशासनकि प्रभाव बहुत गहरे थे। इन सारे इलाक़ों में ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ लागू रहा। गोया बीसवीं सदी को फ़िक़्हे-इस्लामी की जो विरासत मिली, उसमें फ़िक़्हे-इस्लामी के संकलन codification का पहला उदाहरण भी बीसवीं सदी को उन्नीसवीं सदी से मिला। हम निस्संकोच कह सकते हैं कि 1876 ई॰ से लेकर 1925 ई॰ तक का ज़माना ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ के राज का ज़माना है। इस दौरान विस्तृत पैमाने पर मुजल्ले का अध्ययन किया गया, मुजल्ले की अनेक शरहें (व्याख्याएँ) अरबी और तुर्की भाषाओं में लिखी गईं। उनमें से एक लोकप्रिय व्याख्या लेबनान के एक मसीही क़ानूनविद् सलीम-बिन-रुस्तम बाज़ की लिखी हुई भी थी। मुजल्ले की दो महत्त्वपूर्ण शरहें उल्लेखनीय हैं। एक अल्लामा अली हैदर की है जो मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी और तुर्की से अरबी में अनुवाद हुई। यह व्याख्या चार मोटी जिल्दों और लगभग तीन हज़ार पृष्ठों पर आधारित है। यह व्याख्या कई बार छप चुकी है। दूसरी व्याख्या अल्लामा ख़ालिद अल-अतासी की है जो पाँच भागों में है। उसका उर्दू अनुवाद भी उपलब्ध है।
बीसवीं सदी में फ़िक़्ह के अध्ययन का एक नया आयाम
उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के आरम्भ से मुस्लिम जगत् में बड़ी संख्या में क़ानून विशेषज्ञों ने पश्चिमी क़ानूनों का अध्ययन शुरू किया। उनमें वे क़ानून विशेषज्ञ भी शामिल थे जो फ़िक़्हे-इस्लामी की भी जानकारी रखते थे और उन्होंने पश्चिमी क़ानूनों का भी गहराई से अध्ययन किया था। उदाहरण के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में सर सैयद अमीर अली थे। सर सैयद अमीर अली मूल रूप से एक वकील थे। मुसलमानों में चोटी के वकीलों में शुमार होते थे। वे सम्भवत: पहले मुसलमान थे जो अंग्रेज़ी हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए। फिर शायद वही पहले मुसलमान थे जो प्रिवी कौंसिल के जज नियुक्त हुए। यह इंग्लैंड की सबसे बड़ी अदालत थी। अब भी सबसे बड़ी अदालत है। सैयद अमीर अली उसके पहले मुसलमान जज थे। इसलिए अंग्रेज़ी क़ानून में तो उनकी दक्षता निस्सन्देह शक-सन्देह से परे थी। उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ-साथ अरबी और फ़ारसी भी पढ़ी थी। इस्लामी ज्ञान से उनको दिलचस्पी थी। इसलिए उन्होंने निजी अध्ययन से फ़िक़्हे-इस्लामी में भी ख़ासी जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी पर एक दो किताबें लिखीं और इस्लाम के सामान्य परिचय पर एक किताब लिखी जो ‘स्प्रिट ऑफ़ इस्लाम’ (The spirit of Islam) के नाम से कई बार छपी है। इसके उर्दू और अरबी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। इस किताब के द्वारा पहली बार पश्चिमी दुनिया ने इस्लाम के दृष्टिकोण को किसी मुसलमान की भाषा से सुना। अगरचे हर इंसान की तरह सर सैयद अमीर अली के विचारों से भी मतभेद किया जा सकता है। मुझे स्वयं कई अवसरों पर उनके लेखों में कुछ और बेहतरी और सुधार की गुंजाइश महसूस होती है। अनेक समस्याओं के बारे में विद्वानों को उनके मत पर सन्तोष नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से वे हम सबके आभार एवं प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद इस्लाम और मुसलमानों के मत को बयान करना अपनी ज़िम्मेदारी समझा और इस्लाम से सम्बन्धित जो भी उनकी समझ थी, जिससे कहीं-कहीं मतभेद किया जा सकता है, उसके अनुसार उन्होंने इस्लाम के दृष्टिकोण को अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ी में रखा।
इसी तरह से एक और मुसलमान क़ानूनविद् सर अबदुर्रहीम ने, जिनका सम्बन्ध भी कलकत्ता से था, इस्लाम के दृष्टिकोण को एक नए ढंग और शैली से पेश किया। उन्होंने इस्लाम के उसूले-क़ानून (क़ानूनी सिद्धान्तों) पर एक किताब लिखी जो अंग्रेज़ी भाषा में अपने प्रकार की पहली किताब है (Principles of Muhammadan Jurisprudence)। यह इस दृष्टि से एक बड़ी महत्त्वपूर्ण किताब है कि अंग्रेज़ी भाषा में इस्लाम के सिद्धान्तों एवं विचारधारा पर वह पहली किताब है। प्रिंसिपल्ज़ ऑफ़ मुहम्मडन जूरिसप्रुडेंस लिखनेवाला अरबी भाषा से किसी हद तक और फ़ारसी और उर्दू से बड़ी हद तक परिचित था। लेखक को फ़िक़्हे-इस्लामी की काफ़ी कुछ जानकारी थी। अंग्रेज़ी भाषा पर भरपूर पकड़ थी। अंग्रेज़ी क़ानून के बहुत बड़े माहिर थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में, अंग्रेज़ी शब्दावलियों, और अंग्रेज़ी वर्णन शैली में उसूले-फ़िक़्ह के पक्ष और मत को पहली बार पश्चिमी दुनिया के सामने रखा। यह एक नई पहल थी जो फ़िक़्हे-इस्लामी के इतिहास में उन्नीसवीं सदी के आख़िरी दौर से शुरू हुई और बीसवीं सदी में अपने चरम को पहुँची।
अब स्थिति यह थी कि एक-एककर मुस्लिम जगत् में पश्चिमी क़ानून लागू हो रहे थे। इस्लामी क़ानून एक-एककर समाप्त किए जा चुके थे। जो इक्का-दुक्का इस्लामी क़ानून शेष रह गए थे वे भी अब तेज़ी से समाप्त किए जा रहे थे। इस्लामी शिक्षा की संस्थाएँ एक-एककर बंद हो रही थीं। मुसलमानों के सामूहिक, राजनैतिक तथा आर्थिक मामले सब-के-सब पश्चिमी क़ानूनों के तहत चल रहे थे। अरब दुनिया में फ़्रांसीसी क़ानूनों के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज़ी क़ानूनों के अनुसार, मध्य एशिया में रूसी क़ानूनों के अनुसार, इंडोनेशिया में वलनदीज़ी क़ानूनों के अनुसार और जहाँ-जहाँ जिस पश्चिमी ताक़त को क़ब्ज़े का मौक़ा मिला, वहाँ उस पश्चिमी ताक़त के क़ानूनों के अनुसार देश की व्यवस्था चल रही थी। ज़ाहिर है कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम समय और बीसवीं सदी के शुरू में तो मुसलमान इस योग्य नहीं थे कि इस्लामी क़ानूनों को लागू करने की माँग कर सकें, या शरीअत के पुनरुत्थान और इस्लामी फ़िक़्ह को लागू करने के बारे में सोच भी सकें।
फ़िक़्हे-इस्लामी के नए सिरे से अध्ययन की आवश्यकता
जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बेहतर होनी शुरू हुईं और मुसलमान विद्वानों ने बदली हुए परिस्थितियों में शरीअत के आदेशों को लागू करने और इसकी प्रक्रिया पर ग़ौर करना शुरू किया तो यह माँग सामने आती गई कि नई परिस्थितियों में इस्लामी क़ानूनों पर नए ढंग से ग़ौर करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का एहसास बहुत-से लोगों को हुआ। लेकिन मुस्लिम जगत् के जिस महान व्यक्तित्व ने बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इस आवश्यकता को महसूस किया वे अल्लामा इक़बाल थे। उन्होंने 1925 में यह लिखा कि “मेरे नज़दीक इस्लाम इस समय ज़माने की कसौटी पर कसा जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि क़ुरआनी आदेशों के चिरस्थायी होने को साबित किया जाए और जो व्यक्ति वर्तमान के न्यायशास्त्र पर आलोचनात्मक निगाह डालकर यह साबित करेगा कि क़ुरआनी आदेश चिरस्थायी शान रखते हैं, वह मानव जाति का सबसे बड़ा सौन्दर्य और आधुनिक काल का सबसे बड़ा मुजद्दिद* होगा।”
[*मुजद्दिद एक इस्लामी शब्दावली है, जिससे अभिप्रेत वह इस्लामी विद्वान है जो एक शताब्दी के आरम्भ में अपने ज्ञान एवं विचारधारा से इस्लाम का नवीनीकरण करता है——अनुवादक]
अल्लामा इक़बाल के नज़दीक इस काम का जो महत्त्व था उसका अंदाज़ा ही उनके इस लेख से भली-भाँति हो जा रहा है। वे स्वयं यह समझते थे कि इस काम को मुस्लिम जगत् की ज्ञानपरक योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान पर होना चाहिए। शरीअत के अध्ययन के इस पहलू पर लम्बे चिन्तन-मनन के बाद वे इस परिणाम पर पहुँचे कि इस महान कार्य का बेड़ा उनको स्वयं ही उठाना चाहिए। ज़ाहिर है कि अपनी असाधारण अन्तर्दृष्टि, क़ानूनदानी, अरबी और अंग्रेज़ी की जानकारी की वजह से, और सबसे बढ़कर इस वजह से कि सबसे पहले उन्हीं को इस ज़रूरत का एहसास हुआ, वे दूसरों से कहीं बढ़कर इस काम को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने यह चाहा कि अपने तौर पर इस काम को करने के बजाय, इसको सामूहिक रूप से किया जाए। चुनाँचे उन्होंने अपने ज़माने के बहुत-से विद्वानों से सम्पर्क किया। अपने ज़माने के मशहूर मुहद्दिस अल्लामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी को लिखा कि आप लाहौर आ जाएँ तो मैं और आप मिलकर इस काम को करेंगे। मौलाना शिब्ली नोमानी के बारे में वे चाहते थे कि वे लाहौर आ जाएँ। सैयद सुलैमान नदवी के बारे में उन्होंने चाहा कि वे लाहौर आ जाएँ। ख़ुद अल्लामा इक़बाल ने यह चाहा कि वे किसी ऐसे इलाक़े में जाकर बैठें जहाँ इस्लामी विद्वान भी एकत्र हों और मिलकर इस काम को किया जाए। आख़िर में उन्होंने पूर्वी पंजाब के ज़िला पठानकोट के एक छोटे से गाँव में एक संस्था क़ायम कर दी। उसमें यह तय किया गया कि एक नौजवान मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह॰) को बुलाया जाए। तय यह हुआ कि मौलाना मौदूदी (रह॰) वहाँ रहेंगे। अल्लामा इक़बाल भी साल में छः महीने के लिए वहाँ जाकर रहा करेंगे। और वहाँ बैठकर दोनों लोग अपने सामूहिक प्रयास से युवा विद्वानों को प्रशिक्षण भी देंगे और फ़िक़्हे-इस्लामी के पुनः संकलन का काम भी करेंगे। और यों आधुनिक काल की आवश्यकताओं के अनुसार तथा पश्चिमी धारणाओं या पश्चिमी संस्थाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए फ़िक़्हे-इस्लामी के नियमों एवं सिद्धान्तों को नए सिरे से संकलित किया जाएगा।
इसकी शक्ल अल्लामा इक़बाल के ज़ेहन में क्या थी, वे किन दिशा-निर्देशों पर यह काम करना चाहते। इसके बारे में निश्चित रूप से अनुमान करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि इस विषय पर उनका कोई लेख मौजूद नहीं। लेकिन सम्भवतः वे यह चाहते थे कि इस्लामी क़ानूनों को इस तरह से संकलित किया जाए कि उनके अपने शब्दों में क़ुरआनी आदेशों का शाश्वत होना साबित हो। आधुनिक काल की jurisprudence (न्यायशास्त्र) पर आलोचनात्मक निगाह डाली भी गई हो और उसकी कमज़ोरियों को उजागर भी किया गया हो। अल्लाह तआला को शायद यह स्वीकार नहीं था कि यह काम उस समय पूर्णता को पहुँचे, या इसके लिए अभी समय नहीं आया था। जब मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह॰) हैदराबाद दक्कन (दक्षिण भारत) में अपना घर-बार छोड़कर, मकान आदि बेचकर और सब कुछ समेटकर हैदराबाद से लाहौर पहुँचे तो यह सम्भवतः जनवरी 1938 ई॰ की घटना है। वे अल्लामा इक़बाल से मिलते हुए पठानकोट गए। लाहौर में कई दिन उनसे मुलाक़ातें करते रहे। यह तय हुआ कि अल्लामा इक़बाल का स्वास्थ्य जैसे ही सुधरेगा वे पठानकोट का सफ़र करेंगे। लेकिन अप्रैल 1938 ई॰ में अल्लामा इक़बाल का इन्तिक़ाल हो गया। इस काम की न तो आरम्भिक रूपरेखा ही तैयार हो सकी और न काम का आरम्भ ही हो सका। इससे यह स्पषट करना अभीष्ट है कि मुस्लिम जगत् के इस महान सुपुत्र और चिन्तक की दृष्टि में इस काम का कितना महत्त्व था।
बीसवीं शताब्दी में मुस्लिम जगत् के अन्दर भी और बाहर भी पश्चिमी क़ानूनों से इस्लामी क़ानूनों के टकराव का सिलसिला जारी रहा। यह टकराव सकारात्मक ढंग का भी था और नकारात्मक ढंग का भी था। नकारात्मक ढंग का टकराव तो यह था कि पश्चिमी जगत् के अनगिनत लोगों ने और उनके प्रभाव से पूर्वी जगत् में बहुत-से लोगों ने इस्लामी क़ानूनों के बारे में नकारात्मक बातें कीं, आपत्तियाँ कीं और बहुत-से सन्देह पैदा किए। इसकी प्रतिक्रिया में इस्लामी विद्वानों और फ़ुक़हा ने इस्लाम के पक्ष को बहुत विस्तार के साथ और नए ढंग से बयान किया।
सकारात्मक पहलू यह था कि पश्चिमी क़ानून चूँकि पिछले चार-पाँच सौ वर्ष से दुनिया में लागू हैं और आधुनिक काल के जितनी अभिवृद्धियाँ और विकास हैं, पश्चिमी क़ानून उनके साथ-साथ चल रहे हैं। इसलिए पश्चिमी क़ानूनों में कुछ मौलिक धारणाएँ ऐसी मौजूद हैं जो केवल आधुनिक काल की अपेक्षाओं को देखते हुए सामने आईं। इन अनुभवों की रौशनी में फ़िक़्हे-इस्लामी के मत को बयान करना तुलनात्मक रूप से आसान हो गया। फिर आधुनिक काल में जीवन का जो विभाजन हुआ है। राज्य की व्यवस्था जिस तरह से संकलित हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों ने जो-जो शक्लें अपनाई हैं, पश्चिमी क़ानून उन धारणाओं और शक्लों के अनुसार ख़ुद-ब-ख़ुद ढलते चले गए। अब मुसलमानों के लिए बहुत आसान है कि इन तमाम शक्लों और धारणाओं के बारे में फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष और मत बयान कर सकें। जैसे अगर किसी काग़ज़ या कपड़े पर आपको कोई आकृति बनानी हो और कोई व्यक्ति पेंसिल से उसपर रेखाचित्र बना दे, अब आपका काम केवल रंग भरना हो तो यह काम बहुत आसान हो जाता है। गोया पेंसिल से बड़ी हद तक रेखाएँ खींची जा चुकी हैं। अब उस रेखाचित्र के अन्दर फ़िक़्हे-इस्लामी, पवित्र क़ुरआन, सुन्नत और मुसलमानों के फ़िक़्ही भंडार से रंग भरना है। और जहाँ-जहाँ आंशिक बदलाव करना अनिवार्य हो वह करना है। अब यह काम तुलनात्मक रूप से आसान हो गया है। यह पश्चिमी क़ानूनों का आंशिक रूप से सकारात्मक पहलू है। इसने फ़िक़्ह इस्लामी को एक नया आयाम दिया।
फ़िक़्हे-इस्लामी का नया दौर
बीसवीं सदी की आख़िरी तीन चौथाइयाँ और विशेषकर उसका दूसरा अर्द्ध भाग फ़िक़्हे-इस्लामी में एक नए दौर का आरम्भ है। अरब दुनिया में विशेषकर और ग़ैर-अरब दुनिया में आम तौर पर फ़िक़्हे-इस्लामी पर एक नए ढंग से काम का विशाल स्तर पर आरम्भ हुआ। ऐसा काम जो उन लोगों के लिए था जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोग और मुसलमानों में वे लोग थे जो पश्चिमी क़ानूनों और विचारों से परिचित एवं प्रभावित हैं। यह काम अरब दुनिया में अधिक सफलतापूर्वक हुआ। ग़ैर-अरब दुनिया में इतनी सफलता के साथ नहीं हुआ। इसके शायद दो कारण हैं।
पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कारण तो यह मालूम होता है कि पश्चिमी दुनिया में भाषा और दूरी कोई समस्या नहीं थी और न ही भाषा आधुनिक एवं प्राचीन दोनों वर्गों के बीच कोई रुकावट थी। हमारे यहाँ भाषा की रुकवट सबसे बड़ी रुकावट थी जिसकी वजह से आधुनिक और प्राचीन दोनों वर्गों के मध्य एक बड़ी खाई आ गई थी। मुस्लिम उलमा अंग्रेज़ी नहीं जानते और क़ानूनविद् लोग अरबी से परिचित नहीं। इसलिए न उलमा अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं, न वे अपनी बात उलमा तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए दोनों के दरमियान कोई meeting point नहीं था। हमारे यहाँ के विपरीत अरब दुनिया में पश्चिमी क़ानून अरबी में अनुवादित होकर लागू हुए। इस दृष्टि से वे हमसे बेहतर थे कि उन्होंने अपनी ज़बान नहीं छोड़ी। पश्चिमी क़ानूनों का पहले अपनी भाषा में अनुवाद किया और फिर उनको लागू किया। उन्होंने क़ानून के बारे में जो कुछ सोचा और जो कुछ लिखा वह अरबी ही में लिखा। अरबी में सोचने और लिखने के दो लाभ ऐसे हुए जो हमारे यहाँ नहीं हो सके। एक लाभ तो यह हुआ कि अरबी ज़बान का अपना एक स्वभाव है जिससे इस्लामी स्प्रिट को अलग नहीं किया जा सकता। जब पश्चिमी क़ानूनों को अरबी में लिखा गया तो कुछ-न-कुछ इस्लामी आत्मा और इस्लामी स्वभाव उन पश्चिमी क़ानूनों में भी दाख़िल हो गया। दूसरा लाभ यह हुआ कि चूँकि अरब दुनिया के क़ानूनविद् लोग सारा काम अरबी ही में कर रहे थे तो वह फ़िक़्हे-इस्लामी से इतने अपरिचित और इतने दूर नहीं थे जितना हमारा वह वर्ग जो अंग्रेज़ी ही लिखा, पढ़ता और बोलता है और अरबी से बिल्कुल अनभिज्ञ और शरीअत से अपरिचित है।
आज तो अंग्रेज़ी में इस्लाम पर अनगिनत किताबें आ गई हैं। तमाम सिहाहे-सित्ता का अंग्रेज़ी अनुवाद मौजूद है। इस्लाम पर हज़ारों किताबें ख़ुद मुसलमानों की लिखी हुई मौजूद हैं। आज से सौ वर्ष पहले का वातावरण देखें जब मुसलमानों के हाथ की लिखी हुई अच्छी किताबों की संख्या दो-चार से अधिक नहीं होगी। इसलिए वह वर्ग जो अंग्रेज़ी परिवेश का पला-बढ़ा और अंग्रेज़ी संस्थाओं का तैयार किया हुआ था, वह इस्लाम को समझने और उसके अध्ययन की हद तक उतना ही दूर था जितना कोई अंग्रेज़। इसलिए हमारे यहाँ इस वर्ग में इस्लाम और फ़िक़्हे-इस्लामी के बीच जो फ़ासला पैदा हुआ था वह समय के साथ-साथ बढ़ता चला गया, कम नहीं हुआ।
इसके विपरीत अरब दुनिया में अगर इन दोनों वर्गों के मध्य कोई दूरी थी तो वह भी समय के साथ-साथ कम होती चली गई। एक तो समकालीन इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने पश्चिमी ढंग पश्चिमी शब्दावलियों, नई शैली और नए मुहावरे में फ़िक़्हे-इस्लामी पर किताबें लिखीं। उनका सम्बोधन उन्हीं लोगों से था जो क़ानूनविद्, वकील और जज लोग थे। दूसरी तरफ़ उन क़ानूनविदों और जजों ने अरबी भाषा की गहराई और प्रत्यक्ष रूप से जानकारी की वजह से वह दूरी महसूस नहीं की जो उनको फ़िक़्हे-इस्लामी से हो सकती थी, अगर वह अरबी भाषा न जानते। इसलिए यह काम अरब दुनिया में ज़्यादा सफलता के साथ हुआ। कुछ लोगों ने ऐसी असाधारण और इतिहास निर्मित करनेवाली किताबें लिखीं कि उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी का मैदान मुसलमानों के लिए मार लिया। यह बात मैं निस्संकोच कह सकता हूँ कि उन्होंने अरब दुनिया में फ़िक़्हे-इस्लामी का मोर्चा जीत लिया। आज कोई अरब क़ानूनविद् कम-से-कम पिछले तीस-पैंतीस वर्ष से यह नहीं कहता कि इस्लामी क़ानून अव्यावहारिक हैं और पश्चिमी क़ानूनों ही को लागू होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है भी तो वह किसी के दिल में होगी या एक-आध प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिनकी बात का कोई ख़ास महत्त्व नहीं है। इस समय अरब दुनिया में क़ानूनविद् लोगों, जजों और वकीलों की बड़ी संख्या वह है जो फ़िक़्हे-इस्लामी के बारे में अत्यन्त सकारात्मक और श्रद्धाभाव रखती है।
अरब दुनिया में बीसवीं सदी के दौरान जो काम हुआ, इस पूरे काम का विश्लेषण करना तो इस संक्षिप्त चर्चा में बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ महत्त्वपूर्ण कामों का उल्लेख करना उचित होगा। सम्भवत: 1940 ई॰ के दशक के अन्त में अरब दुनिया में इस आवश्यकता का एहसास पैदा हुआ कि फ़िक़्हे-इस्लामी को नए ढंग से आधुनिक सोच रखनेवालों के सामने पेश करना चाहिए। यह वह ज़माना था कि विभिन्न अरब देश एक-एककर आज़ाद हो रहे थे। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इराक़ आज़ाद हुआ, सीरिया और लेबनान आज़ाद हुए। मिस्र विश्वयुद्ध से पहले ही आज़ाद हो चुका था और शेष अरब देश भी आज़ादी की नेमत पा रहे थे। अब वहाँ नए क़ानून और संविधान के बनने का मरहला आया और इस सवाल पर ग़ौर होना शुरू हुआ कि अब नए माहौल में संविधान बनाने का काम किस प्रकार किया जाए। नए संविधान में नई अपेक्षाओं के साथ-साथ इस्लामी धारणाओं को कैसे समोया जाए। इन परिस्थितियों में इन इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जो पिछले कई वर्ष से इस्लामी क़ानूनों को नए अंदाज़ में बयान कर रहे थे, यह माँग की कि देश में पश्चिमी क़ानूनों की जगह इस्लामी क़ानून लागू किए जाएँ। इस सिलसिले में जब चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो इस बात की आवश्यकता का एहसास पैदा हुआ कि फ़िक़्हे-इस्लामी के भंडार को नए ढंग से और नए सिरे से संकलित किया जाए। नई धारणाओं और सिद्धान्तों को नहीं, बल्कि पहले से चली आनेवाली धारणाओं और सिद्धान्तों को नए ढंग और नई शैली में पेश किया जाए।
फ़िक़ही रचनाओं का नया अंदाज़
इस मौक़े पर मुस्लिम जगत् के अतिप्रसिद्ध, महान और बीसवीं सदी के सबसे बड़े फ़क़ीह मुस्तफ़ा अहमद ज़रक़ा ने प्रस्ताव पेश किया कि फ़िक़्हे-इस्लामी के संग्रहों और सिद्धान्तों को एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में तैयार किया जाए। जिस तरह इंसाक्लोपीडिया में होता है कि जिस कला का इंसाइक्लोपीडिया होता है उस कला की तमाम धारणाएँ, बहसें और विषय वर्णानुक्रम से (alphabetical) संकलित किए जाते हैं। आप जो चीज़ जानना चाहें उसको वर्णानुक्रम से तलाश कर लें। आपको पूरे विषय का सार मिल जाएगा और नए अध्ययन के लिए और अधिक स्रोत की निशानदेही हो जाएगी। उस्ताद ज़रक़ा का ख़याल था कि अगर ऐसी कोई व्यापक किताब तैयार हो जाए तो वकीलों, जजों और क़ानूनविदों के लिए फ़िक़्हे-इस्लामी की बहसों से लाभान्वित होने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। मुस्तफ़ा ज़रक़ा ने एक इंसाइक्लोपीडिया का नक़्शा बनाया। कुवैत में इसपर काम शुरू हुआ। कई बार रुका और कई बार शुरू हुआ। लेकिन वे ज़िंदगी-भर इस बात की दावत देते रहे और लगभग चालीस-पैंतालीस वर्ष वे इस बात पर लिखते और ज़ोर देते रहे कि एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जाए। चुनाँचे इस विषय पर दो इंसाइक्लोपीडिया तैयार हुए जिनमें से एक के क्रम में स्वयं उस्ताज़ मुस्तफ़ा ज़रक़ा भी शामिल रहे। उन्होंने उसमें बहुत कुछ लिखा। उसके लेख के क्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके कई शिष्य प्रत्यक्ष रूप से उसके क्रम में साझेदार थे। यह एक बेहतरीन इंसाइक्लोपीडिया है और सम्भवतः पैंतालीस या पचास भागों में पूरी हो गई है। कुवैत के औक़ाफ़ मंत्रालय ने, ‘मौसूअतुल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी’ के नाम से यह काम कराया है। कुवैत के वक़्फ़ मंत्रालय ने पच्चीस-तीस वर्ष में इसपर बहुत-से संसाधन ख़र्च किए हैं और अरब दुनिया के बेहतरीन फ़िक़ही दिमाग़ों ने इसकी तैयारी में हिस्सा लिया है। यह इंसाइक्लोपीडिया अरबी भाषा में है। कुवैत की हुकूमत शायद उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करा रही है। लेकिन इस अनुवाद की कार्रवाई का मुझे नहीं मालूम। उर्दू अनुवाद के बारे में भी एक ज़माने में प्रस्ताव आया था और कुछ लोगों ने पाकिस्तान में इसपर काम भी शुरू किया था। लेकिन हमारे यहाँ हर काम निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ जाता है। कुवैत का नाम सुनकर कुछ लोगों ने यह समझा कि बहुत पैसा मिलेगा। इस ख़याल से बहुत-से लोग विभिन्न कारणों के आधार पर मैदान में आ गए, लेकिन यह काम इस मतभेद की भेंट चढ़ गया और पूरा नहीं हो सका। इसका कुछ विवरण जो बहुत दुख-भरा है, मुझे मालूम है। अलबत्ता भारत के विद्वानों ने इस्लामी फ़िक़्ह अकैडमी के प्रबन्ध में इस अद्वितीय किताब के अधिकतर भागों का उर्दू अनुवाद कर डाला है और जो प्रकाशनाधीन है।
बहरहाल यह इंसाइक्लोपीडिया पूरा हो चुका है। अब फ़िक़्हे-इस्लामी के सारे संग्रह में जो मौलिक धारणाएँ, मौलिक सिद्धान्त और विचारधाराएँ हैं, उन सबको बड़े सलीक़े से और ज्ञानपरक ढंग से संकलित कर दिया गया है। अब अरब दुनिया में किसी को कम-से-कम यह कहने का बहाना नहीं रहा कि मेरे पास फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष और मत जानने का कोई ज़रिया नहीं। अब अरब दुनिया का कोई क़ानूनविद् जब चाहे और जिस विषय पर चाहे उसको इमाम शाफ़िई (रह॰) और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) से लेकर आज तक के फ़ुक़हा के काम का पूरा सार एक व्यापक ढंग में मिल जाएगा।
एक दूसरा इंसाइक्लोपीडिया और भी है जो इस दर्जे का तो नहीं है, लेकिन ज्ञानपरक दृष्टि से अच्छा है। यह मिस्र में तैयार हुआ। इसका नाम भी ‘मौसूअतुल-फ़िक्ह अल-इस्लामी’ है। यह नौ या दस भागों में है। क्रम, सामग्री और व्यापकता की दृष्टि से कुवैत का इंसाइक्लोपीडिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मिस्र का इंसाइक्लोपीडिया अगरचे लाभकारी है, मगर इस दर्जे का नहीं। बहरहाल फ़िक़्हे-इस्लामी के विद्यार्थियों को कुवैत सरकार और मिस्र सरकार के साथ-साथ इन सब लोगों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए जिन्होंने इस काम की रूपरेखा बनाई, योजना बनाई, लेख लिखे और इस काम को पूरा किया।
बीसवीं सदी में एक बड़ा काम तो मुस्लिम जगत् में यह हुआ जो फ़िक़्हे-इस्लामी के इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। दूसरा काम जिसके बहुत-से उदाहरण हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों पर ही बस करूँगा। वह यह हुआ कि कुछ बड़े और प्रतिष्ठित इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने यह सोचा कि आधुनिक पश्चिमी धारणाओं को सामने रखते हुए और नई समस्याओं की निशानदेही करके इन समस्याओं के बारे में फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष आधुनिक ढंग से नई शब्दावलियों के साथ बयान किया जाए। इस में दो-तीन काम बड़े नुमायाँ हुए।
एक महत्त्वपूर्ण काम तो मिस्र के अत्यन्त प्रसिद्ध फ़क़ीह और मुजाहिद इस्लाम अब्दुल-क़ादिर औदा शहीद ने किया। यह इख़्वानुल-मुस्लिमून के लीडर थे और 1954 ई॰ में जमाल नासिर ने उनको फांसी देकर शहीद कर दिया था। उनका काम इतना असाधारण है कि कुछ विद्वानों का ख़याल है कि यह किताब यानी ‘अत्तशरीउल-जिनाई अल-इस्लामी मक़ारिनन बित्तशरीइल-वज़ई’, बीसवीं सदी में लिखी जानेवाली फ़िक़्ह की कुछ बेहतरीन किताबों में से है। इस किताब में उस्ताज़ शहीद ने इस्लाम के फ़ौजदारी क़ानून के गहरे ज्ञानपरक अध्ययन के साथ-साथ आधुनिक फ़ौजदारी क़ानून के साथ उसकी सफल तुलना भी की है। यह किताब दो बड़े भागों में है और फ़ौजदारी क़ानूनों पर फ़िक़्हे-इस्लामी के पूरे भंडार में बेहतरीन किताब है। इससे बेहतर कोई किताब फ़िक़्हे-इस्लामी के भंडार में इस्लाम के फ़ौजदारी क़ानून का पक्ष बयान करनेवाली नहीं है। कोई व्यक्ति जो फ़िक़्हे-इस्लामी का विद्यार्थी हो और इस्लाम के फ़ौजदारी क़ानून को समझना चाहता हो, वह इस किताब के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। उसका उर्दू अनुवाद भी हुआ है और अंग्रेज़ी में भी गुज़ारे के योग्य एक अनुवाद मौजूद है। उसके दर्जनों बल्कि शायद सैंकड़ों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।
इसी प्रकार से फ़िक़्हे-इस्लामी की एक महत्त्वपूर्ण समस्या ‘मुशारका’ और ‘मुज़ारबा’ की थी। उसके बारे में मुस्लिम जगत् में यह सर्वसम्मति पाई जाती है कि आधुनिक काल के बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग की अपेक्षाएँ जिस संस्था के द्वारा पूरी हो सकती हैं, वह ‘मुशारका’ और ‘मुज़ारबा’ की संस्था है। ‘मुशारका’ और ‘मुज़ारबा’ को नए ढंग से इस प्रकार संकलित किया जाए और restructure किया जाए कि आजकल जो-जो सकारात्मक कार्य कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग के द्वारा किए जा रहे हैं वे सारे काम ‘मुज़ारबा’ और ‘मुशारका’ के द्वारा किए जा सकें। कॉर्पोरेट यानी सामूहिक कारोबार कैसे होता है? उसके रूप क्या होते हैं? उसके क़ानूनों में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो शरई रूप से आपत्तिजनक हैं और इस्लामी शरीअत से टकराती हैं? कौन-सी चीज़ें हैं जो इस्लामी शरीअत से टकराती नहीं हैं और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आंशिक परिवर्तन से इस्लामी शरीअत के अनुसार किया जा सकता है। यह काम भी एक-दो दिन का नहीं था, बल्कि एक लम्बे समय का काम था। कई लोगों ने मिलकर इस काम को किया। जिन लोगों ने मिलकर इस काम को किया उनमें तीन बड़े नुमायाँ हैं। एक तो मिस्र के एक फ़क़ीह और जामे अज़हर के एक उस्ताद शैख़ अली अल-ख़फ़ीफ़ थे। उन्होंने एक छोटी-सी और संक्षिप्त किताब लिखी ‘अश-शिरकातु फ़िल-फ़िक़्हिल-इस्लामी’ यानी इस्लामी फ़िक़्ह में शिरकात companies in Islamic Law. यह वैसे तो छोटी-सी किताब है लेकिन इसका ज्ञानपरक बौद्धिक महत्त्व बहुत ज़्यादा है। उन्होंने यह किया है कि आजकल के दौर में कम्पनियों की जो व्यवस्था और कार्य-विधि है उसको सामने रखते हुए फ़िक़्हे-इस्लामी के अनुसार कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग के क्या-क्या रूप हो सकते हैं।
इसके बाद दो और लोगों ने भी शिरकात पर किताबें लिखीं। एक हमारे दोस्त डॉक्टर शैख़ अब्दुल-अज़ीज़ ख़ियात हैं, जो उर्दुन (जॉर्डन) के औक़ाफ़ मंत्री भी रहे। उनकी एक किताब दो भागों में है। ‘अश्शिरकातु फ़िल-फ़िक़्ह अल-इस्लामी’ जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा विस्तृत है। शैख़ अब्दुल-अज़ीज़ अल-ख़ियात, शैख़ अली अल-ख़फ़ीफ़ और कई दूसरे लोगों ने मिलकर वह काम किया जिससे एक मज़बूत ज्ञानपरक आधार बन गया और बाद में आनेवालों ने बड़ी संख्या में इस्लाम के पूरे कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग की कल्पना को एक नए ढंग से संकलित कर दिया।
जब इस्लाम में कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग की धारणा एक नए ढंग से संकलित हो गई तो अब शेष मामलों पर काम करना आसान हो गया। चुनाँचे इस्लामिक बैंकिंग, इंशोरेंस, फ़ाइनांसिंग, बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, पूँजी निवेश, इन समस्याओं के बारे में नई धारणाए सामने आनी शुरू हुईं। बीसवीं सदी का मध्य इन धारणाओं के पुष्ट होने का ज़माना था। ये धारणाएँ समय के साथ-साथ निखरती और पुष्ट होती चली गईं। हर नए आनेवाले ने इसपर कुछ और ग़ौर किया और पिछले लोगों के काम में जो कसर रह गई उसको दूर किया और बेहतर अंदाज़ से काम किया। 1970 के दशक के अन्त और 1980 के दशक के आरम्भ में मुस्लिम जगत् के विभिन्न देशों में व्यवहारतः वे कोशिशें शुरू हुईं कि इस्लामी बैंकिंग और इस्लामी इंशोरेंस की विभिन्न कम्पनियाँ क़ायम की जाएँ। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, पाकिस्तान और सूडान वग़ैरा में ऐसी कोशिशें हुईं।
फ़िक़ही समस्याओं पर सामूहिक चिन्तन
अब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इस सारे काम का जायज़ा लेकर विस्तृत क़ानून संकलित किए जाएँ और व्यावहारिक रूप से निर्देश तैयार किए जाएँ कि इस काम को शुरू कैसे किया जाए और आइन्दा इन संस्थाओं को कैसे चलाया जाए। चुनाँचे अब इस काम का एक सामूहिक रूप सामने आया। सबसे पहले ‘राब्ता-ए-आलमे-इस्लामी’ ने मक्का मुकर्रमा में एक फ़िक़्ह अकैडमी क़ायम की। इसमें मुस्लिम जगत् के विभिन्न इलाक़ों के प्रसिद्ध फ़ुक़हा को जमा किया गया और ये तमाम समस्याएँ उनके सामने रख दी गईं और उनसे कहा गया कि वे अब एक व्यावहारिक नियमावली और दिशानिर्देश तैयार करें जिनमें हर चीज़ के बारे में अलग-अलग बताया गया हो कि क्या करना है।
राब्ता-ए-आलमे-इस्लामी एक ग़ैर-सरकारी संस्था है। इसलिए उसकी फ़िक़्ह अकैडमी ने जो मश्वरे दिए और जो दस्तावेज़ात तैयार कीं उनकी हैसियत भी एक ग़ैर-सरकारी और प्राइवेट प्रकार की थी। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि सऊदी अरब और दूसरे कई देशों में काम करनेवाली इन ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ सरकारी तौर पर भी मुस्लिम जगत् में एक साझी संस्था क़ायम की जाए। चुनाँचे इस्लामी देशों की तंज़ीम OIC ने एक फ़िक़्ह अकैडमी क़ायम की। इसमें हर मुस्लिम देश से दो-दो प्रतिनिधि लिए गए। इन दो-दो प्रतिनिधियों के अलावा मुस्लिम जगत् से बाहर के भी कई बड़े फ़ुक़हा उसके सदस्य हैं। यह जो ‘अल-मजमउल-फ़िक़्ही’ ओआईसी के तहत जिद्दा में काम कर रही है उसने इस मामले में बहुत काम किया है। और बड़े पैमाने पर इन समस्याओं पर विचार व्यक्त किए जो आज मुसलमानों के सामने हैं।
एक व्यापक फ़िक़्ह का जन्म
बीसवीं सदी का आख़िरी चौथाई फ़िक़्हे-इस्लामी पर एक नए अंदाज़ से काम करने का ज़माना है। यह वह ज़माना है कि मुस्लिम जगत् में विभिन्न देशों में एक-एक करके इस्लामी क़ानून लागू किए जाने लगे। पाकिस्तान, ईरान, सूडान, ब्रुनेई और मलेशिया में और अन्य कई देशों में इस्लामी क़ानून लागू किए जाने का काम गंभीरता से आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब जहाँ-जहाँ इस्लामी क़ानूनों की बात हुई वहाँ इस्लामी क़ानूनों पर आपत्तियाँ भी हुईं। ये आपत्तियाँ पश्चिम ने भी कीं और मुस्लिम जगत् के अन्दर से भी हुईं। उन आपत्तियों का प्रकार हर जगह लगभग एक जैसा था। उदाहरणार्थ औरतों के बारे में, ग़ैर-मुस्लिमों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हर जगह लगभग एक ही तरह की आपत्तियाँ की गईं। चूँकि आपत्तियाँ एक जैसी थीं इसलिए उनका जवाब भी एक जैसा दिया गया। जब जवाब एक जैसा दिया गया तो मुस्लिम जगत् के लोगों ने एक-दूसरे से लाभ उठाना शुरू किया। ईरान के अनुभव से पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान से सूडान ने लाभ उठाया। सऊदी अरब से मिस्र ने लाभ उठाया। इसका परिणाम यह निकला कि फ़िक़ही मसलकों की जो सीमाएँ थीं वे एक-एक करके धुँधलाने लगीं। अब समय गुज़रने के साथ-साथ मुस्लिम जगत् में परस्पर सलाह-मशवरा और साझे अमल से यह इज्तिहादी काम किया जा रहा है। इस सामूहिक इज्तिहाद के परिणामस्वरूप फ़िक़ही मसलकों की सीमाएँ मिट रही हैं। एक नई फ़िक़्ह अस्तित्व में आ रही है जिसको न फ़िक़्हे-हनफ़ी कह सकते हैं न मालिकी, न हंबली, न जाफ़री। बल्कि उसको इस्लामी फ़िक़्ह ही कहा जाएगा। मैं इसके लिए Cosmopolitan Fiqh यानी आलमी या ‘हर देसी फ़िक़्ह’ की शब्दावली प्रयुक्त करता हूँ।
उदाहरण के रूप में पाकिस्तान में बैंकिंग की व्यवस्था को इस्लामी साँचे में ढालने का काम 1980 ई॰ में शुरू हुआ।1980 ई॰ में इस्लामी नज़िरयाती कौंसिल ने एक रिपोर्ट पेश की जो इस महत्त्वपूर्ण विषय पर एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट की तैयारी में बैंकिंग विशेषज्ञ भी शामिल थे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के इकनॉमिक्स के विभागों के उस समय के प्रमुख इस रिपोर्ट की तैयारी में शरीक थे। इस्लामी विद्वानों शीया, देवबन्दी, बरेलवी, अहले-हदीस और कोई मसलक न रखनेवाले सब आलिमों ने मिलकर उसके साथ मतैक्य किया। यह रिपोर्ट 1980 में पाकिस्तान सरकार को पेश की गई। यह रिपोर्ट एक ख़ालिस फ़िक़ही मसले के बारे में थी। इस मसले पर कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था से ब्याज को कैसे समाप्त किया जाए और किन चरणों में समाप्त किया जाए। यह रिपोर्ट अर्शशास्त्रियों, क़ानूनविदों, शरीअत के विद्वानों सबके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की हुई है। यह मुस्लिम जगत् के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक फ़िक़्ही और क़ानूनी समस्या पर मुस्लिम जगत् में उपलब्ध तमाम दक्षताओं ने और विभिन्न दृष्टकोण रखनेवाले लोगों ने एक सर्वसम्मत राय पेश की। ज़ाहिर है कि यह रिपोर्ट मात्र फ़िक़्हे-हनफ़ी के आधार पर नहीं है और न इस दस्तावेज़ फ़िक़्हे-हनफ़ी के लिट्रेचर का हिस्सा क़रार दिया जा सकता है। इस तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह फ़िक़्हे-शाफ़िई के आधार पर तैयार हुई है। यह फ़िक़्हे-ज़ैदी या फ़िक़्हे-जाफ़री के आधार पर भी नहीं है। यह पूरी इस्लामी फ़िक़्ह के आधार पर है। इसलिए तमाम फ़ुक़हा और तमाम फ़िक़्ही मसलकों के माननेवालों ने इससे सहमति जताई है। इसका अरबी, मलियालम, बंगला और उर्दू में अनुवाद हुआ और दुनिया में हर जगह इससे लाभ उठाया गया।
इस एक उदाहरण से यह अन्दाज़ा होगा कि अब तक जो पहल हुई है उसमें किसी निर्धारित फ़िक़्ही मसलक के पालन पर बाध्य नहीं किया गया। यों भी वर्तमान परिस्थितियों में किसी निर्धारित फ़िक़्ही मसलक का पालन पब्लिक लॉ की हद तक बहुत मुश्किल है। इसका कारण यह है कि विभिन्न फ़िक़्हों में कुछ ऐसे इज्तिहादात पाए जाते हैं जो आज के दौर में मुश्किल मालूम होते हैं। जबकि दूसरी फ़िक़्ह में उसका हल मौजूद होता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ज़ाहिर है कि इस्लामी फ़ुक़हा ने जब ये इज्तिहादात संकलित किए थे तो ये समस्याएँ और ये परिस्थितियाँ और मुश्किलें तो उनके सामने नहीं थीं। उन्होंने एक दूसरे माहौल में ये इज्तिहादात संकलित किए थे। इसलिए जहाँ परिस्थितियों के बदलने से राय बदलनी चाहिए वहाँ उस राय पर नए सिरे से ग़ौर करना चाहिए। उदाहरणार्थ एक सवाल यह पैदा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई वादा कर ले कि मसलन वह आपसे आपकी फ़ैक्टरी के उत्पादन ख़रीद लेगा, तो क्या उस वादे की कोई क़ानूनी हैसियत भी है या केवल नैतिक हैसियत है। मैं बता चुका हूँ कि विभिन्न मामलों में दौ हैसियतें होती हैं। एक ‘उसके और लोगों के दरमियान’ कहलाती है, जिसका अदालतें नोटिस लेंगी और फ़ैसला करेंगी। दूसरा पहलू होता है ‘उसके और अल्लाह के दरमियान’। यह मामला आपके और अल्लाह के दरमियान है। इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप जानें और आपका ज़मीर जाने। अल्लाह क़ियामत के दिन आपसे पूछ-गछ करेगा। इस पृष्ठभूमि में यह सवाल उठा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई वादा किया जाए तो उसकी हैसियत क्या है। क्या अदालत द्वारा उसे लागू किया जा सकता है या वह मात्र ईमानदारी के अनुसार अनिवार्य होगा।
इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने कहा कि इस तरह का वादा अदालत के अनुसार पालन के लिए अनिवार्य नहीं है। मैं आपसे वादा करूँ कि आप मेरे घर आएँ तो पुलाव खिलाऊँगा और फिर न खिलाऊँ तो आप अदालत में यह माँग लेकर नहीं जाएँगे कि मुझे मजबूर किया जाए को आपको पुलाव खिलाऊँ। यह बज़ाहिर बहुत उचित बात मालूम होती है कि यह अदालत का मामला नहीं है। अदालत को इसमें दख़ल देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने इस सन्दर्भ में जवाब दिया है कि नहीं, किसी वादे की पाबन्दी नैतिक ज़िम्मेदारी तो है, शरई रूप से भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ईमानदारी का तक़ाज़ा है। सर्वोच्च अल्लाह क़ियामत के दिन आपसे पूछेगा। आप कोई जवाब दे सकें तो दें। अदालतों और हुकूमतों को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं।
इसके विपरीत इमाम मालिक (रह॰) ने फ़रमाया कि अगर किसी वादे के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति किसी ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर ले-ले और उस ज़िम्मेदारी के पूरा न होने की वजह से उसका कोई नुक़्सान हो जाए, तो ऐसे हर वादे का पूरा करना अनिवार्य और ज़रूरी है। अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है और देश का क़ानून ऐसे वादों का अनिवार्य रूप से पालन कराने का प्रबन्ध कर सकता है। अब आप देखें कि यहाँ स्पष्ट रूप से इमाम मालिक (रह॰) एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे जो शायद इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के सामने नहीं था। यह मतभेद सामने रखें। ये दोनों की रायें इज्तिहादी हैं, न पवित्र क़ुरआन में कोई स्पष्ट आदेश है, न हदीस में है। दोनों ने अपने-अपने हालात के अनुसार जो समझा, जो मिसालें सामने थीं, उसके अनुसार उन्होंने बयान कर दिया। अब ये दोनों दृष्टिकोण हैं।
आजकल का जो कारोबार है वह पुराने ज़माने के कारोबार की तरह नहीं है कि दो आदमियों ने मिलकर दुकान खोल ली, या एक आदमी दो, चार या दस आदमियों का माल लेकर क़ाफ़िले में चला गया और जाकर व्यापार करके आ गया। ईमानदार है तो बता दिया कि किसको कितना लाभ मिला है, जिसका यह हिसाब है। कभी-कभी लोग अपना एक आदमी भी साथ कर दिया करते थे कि वह देखता रहे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकर स्थिति यह है कि कोई कारोबार ऐसा नहीं जिसमें लाखों-करोड़ों आदमी एक वक़्त में शरीक न हों। बड़े-बड़े कारोबारों के शेयर्स दस-दस रुपये में मिल जाते हैं। उस शेयर को जिसका जी चाहे ख़रीदे। अगर बैंकों को ‘मुज़ारबा’ कम्पनियों के तौर पर चलाना है तो जितने खाताधारक हैं वे इस ‘मुज़ारबा’ में शरीक होंगे और सब ‘रब्बुल-माल’ (माल के मालिक) होंगे। पाकिस्तान में सम्भवतः तीन-साढ़े तीन करोड़ खाताधारकों के कारोबार में यह कहाँ सम्भव है कि एक आदमी यह देखने के लिए रखा जाए कि कारोबार सही हो रहा है कि नहीं। यह स्थिति है। इसलिए इसपर नए सिरे से ग़ौर करना पड़ेगा।
इतने बड़े पैमाने पर जो कारोबार होता है उसकी शक्ल यह होती है कि मान लीजिए आप कोई कम्पनी लॉन्च करना चाहते हैं। दुनिया में आजकल जो क़ानून हर जगह प्रचलित है वह यह है कि आप पहले उस कम्पनी की कल्पना अपने ज़ेहन में स्पष्ट करें जो आप बनाने जा रहे हैं। उस कम्पनी का एक मौलिक ढाँचा तैयार करें जो मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन कहलाता है। इसमें आप स्पष्ट रूप से यह बताएँगे कि वह कम्पनी क्या करेगी। इसमें आप कितनी पूँजी लगाना चाहते हैं। कितने पैसे आप अभी देने के लिए तैयार हैं और कितने बाद में देंगे। आप शेयर्स के नाम पर पब्लिक से कितने पैसे लेना चाहते हैं। एक को-अथोराइज़्ड कैपिटल या अनुमति प्राप्त पूँजी कहते हैं और दूसरे को पेड-अप कैपिटल या चुकाई गई पूँजी कहते हैं। पेड-अप कैपिटल कितना होगा और अथोराइज़्ड कैपिटल कितना होगा। जो मूल पूँजी आप लगा रहे हैं वह कितनी होगी। किसी और व्यक्ति ने अगर ज़िम्मा लिया है जिसको अंडर-राइटिंग कहते हैं, वह कौन व्यक्ति है और उसने कितना ज़िम्मा लिया है। अगर उसने कुछ शर्तों रखी हैं तो वे क्या हैं। यह काम करने के बाद आपको वह कम्पनी सरकार के पास रजिस्टर करवानी पड़ती है। उसके बाद कम्पनी के articles of association बनाने पड़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि कम्पनी के विस्तृत नियम-क़ानून क्या हैं। फिर हुकूमत के नियम-क़ानून के अनुसार आप इस बारे में समाचारपत्र में विज्ञापन देंगे। उस विज्ञापन के द्वारा आपको बताना पड़ेगा कि कौन-कौन लोग इसमें शरीक हैं। उनकी credibility क्या है। वे कितने लाभ की उम्मीद करते हैं। इसके हिसाब से लोग उसमें पैसा लगाएँगे और पूँजीवादी संस्थाएँ उसमें पैसा देंगी। अब ये अरबों-खरबों का कारोबार होता है। ख़ुद इस एलान के मरहले तक पहुँचने के लिए कई करोड़ ख़र्च करने पड़ते हैं। कई करोड़ या कई लाख रुपये ख़र्च करने के बाद यह मरहला आता है कि आप कम्पनी लॉन्च करने की बात करें।
ख़ालिस हनफ़ी मसलक के दृष्टोकोण से देखें तो यह सब कुछ मात्र एक वादा है। उन्होंने वादा किया कि वे कारोबार शुरू कर रहे हैं। आप पैसा दें तो उसमें लाभ होगा। अब यह वादा, जो उन्होंने किया है, क्या यह बाइंडिंग नहीं है? अगर यहाँ हनफ़ियों का दृष्टिकोण अपनाया जाए, तो इस तरह का कोई कारोबार तो चल ही नहीं सकता। मात्र ऐसे वादे पर जो अदालत की दृष्टि में पालन के लिए अनिवार्य नहीं है और जिसको अदालत लागू नहीं करेगी उसमें कोई आदमी अपना पैसा क्यों लगाएगा। इसपर चिन्तन-मनन शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि इमाम मालिक (रह॰) का दृष्टिकोण यह है कि अगर कोई वादा ऐसा हो कि जिसके परिणामस्वरूप कोई obligation या liability पैदा होती है तो वह वादा पूरा करना अदालत की दृष्टि में अनिवार्य है और अदालत उसके पालन का आदेश देगी। चुनाँचे आजकल के तमाम फ़ुक़हा ने इस राय को अपना लिया। अब जहाँ-जहाँ इस्लामी फ़ाइनांसिंग, बैंकिंग या कम्पनी पर काम हो रहा है वहाँ इमाम मालिक (रह॰) के इसी दृष्टिकोण के अनुसार हो रहा है।
इस एक उदाहरण से यह अनुमान हो जाएगा कि ये इतनी बड़ी और पेचीदा समस्याएँ हैं कि किसी एक फ़िक़्ह के दायरे में रहते हुए उनका समाधान तलाश करना मुश्किल है। कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि चार प्रसिद्ध फ़िक़ही मसलकों के दायरे से निकलकर देखना पड़ा। कुछ जगह प्रत्यक्ष रूप से क़ुरआन और सुन्नत के स्पष्ट आदेशों से दलील लेकर तमाम फ़ुक़हा या ज़्यादा-तर फ़ुक़हा के दृष्टिकोण को नज़रअंदाज करना पड़ा। यह काम इतना आसान भी नहीं है कि हर कोई उसका बेड़ा उठा सके। यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। हर किसी का काम नहीं कि उठकर कहे कि जी मैं चारों फ़ुक़हा के दृष्टिकोण को रद्द करता हूँ। ऐसा दृष्टिकोण जिसपर चार बड़े फ़ुक़हा के ज़माने से लेकर हज़ारों, बल्कि लाखों फ़ुक़हा ने चिन्तन-मनन किया। जो ताबिईन और तबा-ताबिईन के ज़माने के लोग थे। फिर हज़ारों लाखों इंसान लगातार इसपर ग़ौर करते चले आ रहे हैं। कल की चर्चा से अनुमान हो गया होगा कि एक एक शब्द पर सदियों तक ग़ौर हुआ है। इस सारे काम को कोई आदमी आज खड़ा होकर एक बार में कह दे कि जी मैं इसको रद्द करता हूँ। यह इतना आसान काम नहीं। इसमें बहुत विस्तार से चिन्तन-मनन के साथ ईशपरायणता, ज़िम्मेदारी का भाव और सावधानी की आवश्यकता होती है।
फ़िक़्हे-माली और फ़िक़्हे-तिजारत पर नया काम
यह काम बीसवीं शताब्दी की आख़िरी चौथाई में शुरू हुआ और पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान दुनिया के बहुत-से हिस्सों में, मुस्लिम देशों और ग़ैर-मुस्लिम जगत् दोनों में, बड़ी तेज़ी से यह काम होता रहा। अब वह चरण आ गया है कि अमली क़दम उठाए जाएँ। इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ से कम-से-कम इस एक मैदान में, यानी कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग, कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में, जितना आधारभूत ज्ञानपरक कार्य होना था वह लगभग सारे-का-सारा हो गया है। इस काम का एक हिस्सा तो वह है जो हमेशा जारी रहेगा। दूसरा हिस्सा वह है जिसपर परिस्थितियों की दृष्टि से नए सिरे से विचार करना होता रहेगा। लेकिन बहरहाल जितना काम हो गया है उसके द्वारा एक मज़बूत ज्ञानपरक आधार उपलब्ध हो गया है। इस्लामी व्यापार कैसे हो? उसके मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। कारोबार के रूप क्या-क्या हो सकते हैं, इस बारे में दर्जनों, बल्कि सैंकड़ों किताबें और हज़ारों लेख लिखे जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में इसपर लीगर फ़्रेमवर्क जारी हो गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान भी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान ने पिछले साल एक लीगर फ़्रेमवर्क जारी कर दिया है जिसका पालन उन तमाम संस्थाओं को करना पड़ेगा जो इस्लामी बैंकिंग चाहती हैं। इस लीगल फ़्रेमवर्क से बाहर कोई भी संस्था पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग के दावे के साथ काम नहीं कर सकती। इस फ़्रेमवर्क की निगरानी के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान ने एक शरीआ बोर्ड भी क़ायम किया है। यह बोर्ड निजी रूप से हर उस बैंक की निगरानी करता है जो इस्लामी बैंकिंग करना चाहता है। शरीअत के आदेशों के अनुसार जो निर्देश शरीआ बोर्ड देगा वह हर इस्लामी बैंक के लिए फ़ाइनल और पालन के लिए अनिवार्य हैं। यह बहुत बड़ी और महत्त्वपूर्ण पहल है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में जो ज्ञानपरक तैयारी दरकार थी, इसके लिए पिछले चालीस-पचास वर्ष लगातार काम होता रहा।
अब एक और महत्त्वपूर्ण सवाल यह पैदा हुआ कि जब इस्लामी दिशा-निर्देशों पर व्यापारिक संस्थाएँ काम करना आरम्भ करेंगी, वे बैंकिंग की संस्थाएँ हो या नॉन-बैंकिंग संस्थाएँ हों, वे पूँजी निवेश की संस्थाएँ हो या आम संस्थाएँ हों, उनके मामलों, किए हुए कामों और हिसाबात की निगरानी कैसे होगी? इस सवाल के महत्त्व का एक बड़ा कारण यह भी है कि अकाउंटिंग की वर्तमान परिकल्पना हमारे यहाँ पश्चिम से आई है। अकाउंटिंग की तमाम प्रचलित धारणाएँ पश्चिम में पैदा हुईं। अकाउंटिंग का प्रशिक्षण पश्चिमी परिकल्पनाओं और मामलों के अनुसार होता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में इससे सम्बन्धित जो कुछ पढ़ाया जाता है, वह सब पश्चिम से आयातित है। उन धारणाओं और उन दस्तावेज़ात को ज्यों-का-त्यों अपनाकर इस्लामी बैंकिंग की संस्थाएँ चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे अकाउंटेंट्स, जो शरीअत को भी जानते हों और एकाउंटिंग के भी माहिर हों, ऐसी दस्तावेज़ात तैयार करें जिनकी सहायता से इस्लामी बैंकिंग की संस्थाओं की अकाउंटिंग भी हो सके और उनका ऑडिट भी किया जा सके। चुनाँचे इस उद्देश्य के लिए एक संस्था बनाई गई जो Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions कहलाती है। संक्षेप में इसको ‘आयोफ़ी’ कहा जाता है। इस संस्था ने पिछले पंद्रह-बीस वर्ष में लगातार काम किया और ऐसी बड़ी-बड़ी दस्तावेज़ात संकलित करके प्रकाशित कर दी हैं, जो किसी भी संस्था के लिए व्यावहारिक हैं। आपने ISO 9000 का नाम सुना होगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ज़ की संस्था है। आईएसओ ने जो दस्तावेज़ात बनाई हैं इस्लामी अकाउंटिंग की दस्तावेज़ात स्तर में इससे कम नहीं हैं। बिलकुल उसी स्तर के अनुसार हैं। दुनिया के विकसित-से-विकसित माहौल में, बड़ी-से-बड़ी कम्पनी और बड़े-से-बड़े बैंक को अगर इस्लामी बुनियादों पर काम करना हो, तो उसके अकाउंटिंग के तक़ाज़े इन दस्तावेज़ात से पूरे हो सकते हैं। यह काम हो चुका है और पाकिस्तान में शरीआ बोर्ड और स्टेट बैंक ने इन दस्तावेज़ात को अब पाकिस्तान के लिए मोडिफ़ाई करके अपनाने का काम शुरू कर दिया है। यह मोडिफ़िकेशन जो कहीं-कहीं और थोड़ा-थोड़ा दरकार है, यह जैसे-जैसे होता जाएगा तो यह काम भी आसान होता जाएगा।
बज़ाहिर यह एक ख़ालिस कलात्मक कार्य है और इसका फ़िक़्ह से कोई सीधा सम्बन्ध नज़र नहीं आता। लेकिन वास्तव में यह फ़िक़ही प्रकार ही का एक काम है। मैंने पहले बताया था कि एक ज़माने में इल्मुश-शुरूत, इल्मुल-मुहाज़िर और इल्मुस-सजलात के नाम से एक कला अस्तित्व में आई थी, जो नीम-फ़िक़ही (अर्ध-धर्मशास्त्रीय) और नीम-इंतिज़ामी (अर्ध-प्रबन्धनीय) थी। यह काम भी इसी ढंग की चीज़ है। इसमें फ़िक़ही तत्व भी है और प्रयोगात्मक तत्व भी है। आधुनिक काल की आवश्यकता और अपेक्षाओं का तत्व भी है। इसलिए ये नई दस्तावेज़ात अब आनी शुरू हो गई हैं और उपलब्ध हैं।
एक महत्त्वपूर्ण चरण अभी और शेष था जिसपर पिछले दस बारह वर्षों से काम शुरू हुआ है। यह ऑडिट का चरण है। ऑडिट आजकल एक बहुत महत्त्वपूर्ण कला बन गई है। ऐसी-ऐसी फ़र्में हैं जो अरबों रुपये की रक़मों और मामलों का ऑडिट करती हैं और जब तक वे बड़ी-बड़ी कम्पनियों और व्यापारिक संस्थाओं के हिसाबात का ऑडिट न करें, उनका विश्वास बहाल नहीं होता। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं और आप पूँजी निवेश करना चाहते हैं, तो आप रुपया लगाने से पहले यह जानना चाहेंगे कि कौन-सी कम्पनी कैसी है? किसका कारोबार सफल है और किसका नहीं है? कहाँ के लोग ईमानदार हैं और कहाँ के नहीं हैं। यह जानने के लिए ज़रूरी है कि कोई निष्पक्ष संस्था ऐसी हो जिसका उस संस्था से कोई हित न जुड़ा हो और वह स्वतंत्र संस्था स्वतंत्र रूप से व्यापारिक संस्था के हिसाबात की ऑडिट करके बताए कि यह सही है या नहीं। ऑडिटर के लिए अनिवार्य है कि उनके सामने वे दस्तावेज़ात और सिद्धान्त हों जिनके अनुसार उनको ऑडिट करना होता है। इससे शरीआ ऑडिट की धारणा ने जन्म लिया।
शरीआ ऑडिट की धारणा यह है कि उदाहरणार्थ संस्था ‘क’ दावा करती है कि हम ब्याज रहित बैंकिंग पर काम पूर्ण रूप से शरीअत के आदेशों के अनुसार करते हैं और हमारे यहाँ ब्याज रहित पूँजी निवेश होता है। मान लीजिए आपको मुझपर विश्वास है और आपने मुझसे पूछा कि अमुक संस्था ठीक काम कर रही है। क्या हम उसमें पैसा लगा दें? अब मैंने यह मालूम करना चाहा कि यह संस्था क्या काम कर रही है। उन्होंने दस्तावेज़ात और काग़ज़ात के आधार पर लाकर मुझे बता दिया कि वे अमुक-अमुक काम कर रहे हैं जो शरीअत के अनुसार है और उनका काम करने का तरीक़ा यह है। अब मैं तो उनकी दस्तावेज़ात और काग़ज़ देखकर कहूँगा कि वे अपना काम शरीअत के अनुसार ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यवहारतः भी ऐसा ही करते हैं? मैं तो प्रतिदिन जाकर उनके मामलात चेक नहीं कर सकता। इस काम के लिए ज़रूरी है कि प्रति वर्ष संस्था की दस्तावेज़ात चेक करके यह बताया जाए कि इस संस्था ने जो एलान किया था और जो कुछ लिखा था, क्या उसके अनुसार काम हो रहा है? यह बताना ऑडिट का काम है। इसके लिए ऑडिटर्स होने चाहिएँ जो शरीअत को जानते हों। अगर वे यह चेक करें कि कोई संस्था सचमुच ब्याज रहित बैंकिंग के आधार पर काम कर रही है तो वे यह कैसे चेक करेंगे? इसलिए शरीआ ऑडिटके लिए ऐसे ऑडिटर की ज़रूरत है जो शरीअत को भी जानते हों और ऑडिट की कला को भी जानते हों। चुनाँचे शरीआ ऑडिट पर भी काम शुरू हुआ है। उसकी दस्तावेज़ात भी तैयार हुई हैं।
आपको यह सुनकर ख़ुशी होगी कि रमज़ानुल-मुबारक के तुरन्त बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा में इस बारे में एक मीटिंग हो रही है जिसमें दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों से वे लोग बुलाए जा रहे हैं जो इस्लामी बैंकिंग के दीनी या शरई पहलुओं के ज़िम्मेदार हैं। ये लोग मिलकर इस्लामी बैंकिंग के एक महत्त्वपूर्ण पहलू यानी बैंकों की कम-से-कम नक़दी आवश्यकताएँ (minimum adequacy standard) का एक फ़ार्मूला और दस्तावेज़ात मंज़ूर (approve) करेंगे जो पूरे मुस्लिम जगत् में प्रयुक्त हुआ करेंगी। यह मरहला भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होनेवाला है।
यह बीसवीं सदी के अन्त और इक्कीसवीं सदी के आरम्भ के काम हैं जिनमें फ़िक़ही और वैचारिक प्रकार के काम भी हैं और प्रशासनकि और कलात्मक प्रकार के भी। उनमें दस्तावेज़ात की तैयारी के काम भी हैं और इस तरह के व्यावहारिक गाइड लाइंज़ की तैयारी के काम भी हैं जो एक आम आदमी, एक आम बैंकर और एक आम व्यापारी और कारोबारी आदमी प्रयुक्त कर सके। मैंने कारोबार और व्यापार की इस्लामी धारणाओं एवं आदेशों पर अपनी चर्चा में बताया था कि इस समय फ़िक़्हे-इस्लामी का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा यही हो गया है। इसलिए कि इस समय कारोबार और व्यापार की संस्थाओं ने असाधारण महत्त्व अपना लिया है।
राज्य का विकेंद्रीकरण और उसके परिणाम
सौ-डेढ़-सौ वर्ष पहले तक एक ज़माना ऐसा था जब लोगों की ज़िन्दगी में मुख्य भूमिका राज्य की हुआ करती थी। राज्य विचारधारा का ध्वजावाहक और रक्षक होता था। राज्य विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करता था। कम्युनिस्ट राज्य बना। उसने कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश राज्य ने ब्रिटिश विचारधारा को दुनिया में फैलाया और इतना फैलाया कि आज तक दुनिया में फैली हुई है। इसी प्रकार से बड़े-बड़े पश्चिमी राज्यों ने अपनी-अपनी विचाधाराओं और संस्कृति को फैलाया। उस समय के चिन्तकों को यह ख़याल आया कि जिस प्रकार से पश्चिमी राज्य अपनी विचारधारा को फैला रहे हैं, उसी प्रकार एक मज़बूत इस्लामी राज्य स्थापित किया जाए जो इस्लामी विचारधारा को फैलाए और उनको बढ़ावा देने का काम करे, तो इस्लामी विचारधारा को भी इसी प्रकार बढ़ावा मिल जाएगा। इस विचार के तहत बीसवीं शताब्दी के चिन्तकों के निकट इस्लाम राज्य को बहुत महत्त्व प्राप्त हो गया और इस्लाम के पुनरुत्थान के कार्य में इस्लामी राज्य की स्थापना को मूलभूत हैसियत का महत्त्व प्राप्त हो गया। राज्य उनकी विचारधारा का मूल और केन्द्र बिन्दु बन गया। उनका सारा ध्यान इस्लामी राज्य की स्थापना पर केन्द्रित हो गया। लेकिन मुस्लिम जगत् में कोई इस्लामी राज्य स्थापित हुआ कि नहीं हुआ, यह एक अलग मामला है, लेकिन इस सोच का एक सकारात्मक लाभ यह हुआ कि इस्लामी राज्य के बारे में बहुत-सा ज्ञानपरक और शोधपरक कार्य सामने आ गया। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने राज्य के बारे में जो कुछ लिखा था, बीसवीं शताब्दी के बहुत-से विद्वानों ने इसको खंगालकर बहुत-सी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कर दी। दूसरी तरफ़ दुनिया में यह हुआ कि राज्य की केन्द्रीयता समाप्त हो गई। सोवियत यूनियन का पतन हो गया। कम्यूनिज़्म एक विचारधारा के तौर पर दुनिया से समाप्त हो गया। इंग्लैंड का राज्य दुनिया से मिट गया। जहाँ सूर्यास्त नहीं होता था वहाँ अब सूरज निकलता ही नहीं। अब जो बड़ी-बड़ी विचारधाराएँ थीं उनके बढ़ावे के लिए इस तरह के बड़े-बड़े राज्य नहीं रहे जिस तरह कि पहले हुआ करते थे।
अब जो संस्थाएँ अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा दे रही हैं वे मल्टीनेशनल कम्पनियाँ और बड़े-बड़े बैंक हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ़ वे संस्थाएँ हैं जो नॉन-स्टेट संस्थाएँ हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और व्यापार उनके हाथ में है। इस समय दुनिया के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का या मुस्लिम जगत् को कंट्रोल में रखने का जो सबसे बड़ा ज़रिया हैं वे ये मल्टीनेशनल संस्था और कार्पोरेशंज़ हैं। उनके पास दुनिया के आर्थिक जीवन की लगामें हैं। उनके पास दुनिया के आर्थिक संसाधन और वित्तीय ख़ज़ानों की कुंजियाँ हैं। यह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ़ जैसी संस्थाएँ ही हैं जिनके अधिकतर देश ऋणी हैं। और जो ऋणी होता है वह ऋण देनेवाले के क़ब्ज़े में होता है। इसलिए बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जो आगामी पच्चीस-तीस वर्ष या चालीस वर्ष हैं उनमें राज्य की भूमिका मौलिक नहीं होगी, भविष्य का ज्ञान अल्लाह को है, लेकिन अनुमान यह होता है कि आगामी वर्षों में राज्य की भूमिका मौलिक नहीं होगी, बल्कि उन संस्थाओं की भूमिका मौलिक होगी और यह वित्तीय और व्यापारिक संस्था मीडिया और पब्लिसिटी की संस्थाओं के साथ मिलकर मुस्लिम जगत् को कंट्रोल करने का कर्त्तव्य अंजाम देंगे। आगामी नक़्शे में बज़ाहिर ऐसा ही मालूम होता है कि इन्हीं दो संस्थाओं का किरदार मौलिक होगा।
आज के दो बड़े चैलेंज
आज से पचास वर्ष पहले यह बात सम्भव थी कि आप अपने घर में बैठ जाएँ और दुनिया के हर फ़ित्ने से और आपके धर्म एवं संस्कृति प्रभाव डालनेवाली हर चीज़ से सुरक्षित हो जाएँ, लेकिन आज न घर में बैठकर फ़ित्नों से बच निकलना सम्भव है और न ही ऐसी हर चीज़ से सुरक्षित हो जाना सम्भव है। मीडिया के चौतरफ़ा हमले इतनी तेज़ी और शिद्दत से हो रहे हैं कि अल्लाह के घर (काबा) में बैठकर आप दुनिया के दो ढाई सौ चैनल देख सकते हैं। इसलिए यह आशा करना या यह माँग करना कि ये चैनल बंद किए जाएँ और उनको समाप्त किया जाए, एक अवास्तविकतावादी माँग है। ऐसी अव्यावहारिक और अवास्तविक माँग कोई दुरुस्त माँग नहीं। इसलिए कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस स्थिति की रोकथाम होनी चाहिए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसने एक नया चैलेंज मुसलमानों के सामने पेश किया है। पहले चैलेंज का जवाब तो मुसलमान बड़ी हद तक तैयार कर चुके हैं। मल्टीनेशनल कम्पनियों और वित्तीय संस्थाओं का जो चैलेंज है इसमें पहल हो रही है और यहाँ तक पहल हुई है कि अब पश्चिमी संस्था और बैंक भी इस तरफ़ आ रहे हैं। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा बैंक है। हाँगकांग शंघाई बैंक। इंग्लैंड के बैंक ऑफ़ इंगलैंड के बाद दूसरा या तीसरा बड़ा बैंक बताया जाता है। यह बैंक हाँगकांग और शंघाई में रजिस्टर हुआ था लेकिन काम ज़्यादा-तर इंगलैंड में कर रहा है। सुना है कि उसने हाल ही में दो एक वर्ष पूर्व जो इस्लामी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वे बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लगभग दो सौ बिलियन पौंड उसका टार्गेट था कि उसको प्राप्त किया जाएगा। इससे आप अनुमान कर लें कि कितनी बड़ी मार्केट है जो इन इस्लामी संस्थाओं के लिए खुली है। अगर मुसलमान जुर्रत और हिम्मत के साथ इस तरह आएँ तो वे इस काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं।
दूसरे चैलेंज का जवाब देना अभी शेष है और मुसलमानों ने इसपर अभी तक कोई उत्साहवर्धक कार्य नहीं किया। क्या करना चाहिए। यह तो कोई जवाब नहीं कि आप अपने घर पर ताला लगा दें और पर्दा डालकर बैठ जाएँ। सैलाब परदे डालने से नहीं रुकता। सैलाब जब आता है तो वह तालों से नहीं रुकता। इसपर मुसलमानों को विचार करना चाहिए। मुसलमानों में मीडिया के जो विशेषज्ञ हैं वे बताएँ कि इस सिलसिले में क्या कुछ किया जा सकता है।
फ़िक़्हे-इस्लामी की नई किताबें
ये परिस्थितियाँ जिनमें फ़िक़्हे-इस्लामी पर अब नए ढंग की किताबें लिखी जा रही हैं। पुराने ढंग की किताबें जिनका मैंने कल उल्लेख किया था। अब इस प्रकार की किताबें लिखी जाना लगभग बन्द हो गया है। पुराने ढंग की किताब पिछले पचास वर्ष में शायद एक प्रतिशत भी नहीं लिखी गई। अब नए ढंग की किताबें लिखी जा रही हैं। इस समय फ़िक़्हे-इस्लामी को जो संग्रह है, जो गोया बीसवीं शताब्दी के मध्य से आज तक हमारे सामने आना शुरू हुआ है, उसका निन्यानवे (99) प्रतिशत हिस्सा हमारे सामने का लिखा हुआ है। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का एक नया इतिहास या एक नया अध्याय है। कुछ किताबें तो वे हैं जिन फ़िक़्हे-इस्लामी के पक्ष को क़ानूनी धाराओं के रूप में संकलित किया गया। इसका सबसे पहला उदाहरण ‘मुजल्लतुल-अहकाम अल-अदलिया’ है। पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और कई अन्य देशों में बहुत-से क़ानून संकलित हुए हैं जो फ़िक्हे-इस्लामी से लिए गए हैं और इन राज्यों में प्रचलित हैं।
यह फ़िक़्हे-इस्लामी का एक नया नमूना है जो इससे पहले के ज़मानों में नहीं मिलता। ये सारे क़ानून चूँकि फ़िक़्हे-इस्लामी से लिए गये हैं, इसलिए फ़िक़्हे-इस्लामी का हिस्सा हैं। लेकिन इन क़ानूनों की जो व्याख्याएँ लिखी जा रही हैं, इन क़ानूनों पर अदालतें जो फ़ैसले दे रही हैं, इन क़ानूनों पर क़ानूनविदों के वर्गों में जो चिन्तन-मनन हो रहा है, वह एक नए ढंग का काम है। यह सामग्री सारी-की-सारी इस दृष्टि से फ़िक़्हे-इस्लामी का हिस्सा भी है कि वह फ़िक़्हे-इस्लामी की धारणाओं पर आधारित है। और वह आधुनिक क़ानूनों का भी हिस्सा है, क्योंकि इसमें आधुनिक ढंग एवं आधुनिक शैली से काम लिया गया है। गोया एक मिश्रण इन दोनों क़ानूनों में पैदा हो रहा है जो वक़्त के साथ-साथ और पक्का और गहरा होगा। बज़ाहिर अन्दाज़ा यही हो रहा है कि फ़िक़्हे-इस्लामी की आगामी सौ-पचास वर्ष तक की पहल में पश्चिमी क़ानून, पश्चिमी शैली और पश्चिमी तर्क-शैली की मुख्य भूमिका होगी।
आधुनिक काल की फ़िक़्ही किताबों में बहुत-सी किताबें वे हैं कि जिनमें फ़िक़्हे-इस्लामी के पक्ष को पश्चिमी क़ानूनों के अन्दाज़ और शैली के अनुसार संकलित किया गया है। यह काम पाकिस्तान में तो बहुत कम हुआ, लेकिन अरब दुनिया में बहुत विस्तार के साथ हुआ है। इसकी मिसालें दी जाएँ तो बात बहुत लम्बी हो जाएगी। दो तीन किताबों के उदाहरण मैं दिए देता हूँ।
अभी मैंने उस्ताज़ मुस्तफ़ा ज़रक़ा का ज़िक्र किया था। उन्होंने ‘अल-फ़िक़्हुल-इस्लामी फ़ी सौबतिल-जदीद’ के नाम से एक किताब लिखी थी, इसमें उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी को एक नए लिबास में पेश किया है। यह किताब तीन भागों में है। इसमें उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी की मौलिक धारणाओं और उसूले-फ़िक़्ह को पश्चिमी जूरिसप्रुडेंस के अंदाज़ से संकलित किया है। पश्चिमी जूरिसप्रुडेंस पर जो किताबें हैं, उनमें जो क्रम है, जो शैली है या विषयों का जो विभाजन है, उसको अपनाकर उस्ताज़ मुस्तफ़ा ज़रक़ा ने फ़िक़्हे-इस्लामी की सामग्री को उसमें भर दिया है। यों आजकल के अरब क़ानूनविदों के लिए फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष और मत समझना बहुत आसान हो गया है। चाहे यह क़ानूनविद् अमेरिका से पढ़कर आया हो, फ़्रांस या किसी दूसरे देश से लेकिन चूँकि अरबी उसकी मात्र भाषा है इसलिए इस किताब के ज़रिये फ़िक़्हे-इस्लामी का पक्ष समझना उसके लिए अब मुश्किल नहीं रहा।
इस काम में सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और किसी हद तक लेबनान और इराक़ के विद्वानों ने बहुत हिस्सा लिया है। इन लोगों की दिलचस्पी से फ़िक़्हे-इस्लामी के सामान्य परिचय के साथ-साथ क़ानून की अलग-अलग धारणाओं पर किताबें तैयार हुईं। क़ानून की अलग-अलग धारणाओं पर किताबें तैयार करना इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के यहाँ ज़्यादा आम नहीं था। वह इस तरह की किताबें लिखने की शायद न आवश्यकता समझते थे और न इस शैली से ज़्यादा परिचित थे। इसलिए कि क़ानून की धारणाओं पर किताबें लिखने का रिवाज पश्चिमी दुनिया के प्रभाव से मुस्लिम जगत् में आया। उदाहरण के रूप में यह बात कि माल की धारणा क्या है या मिल्कियत किसको कहते हैं, या ‘अहलियत’ यानी competance किसको कहते हैं, इसपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) इस तरह नहीं लिखते थे कि उदाहरणार्थ ‘अहलियत’ पर अलग किताब लिखें और इसमें ‘अहलियत’ के सारे आदेश दर्ज हों, बल्कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की शैली यह थी कि वे फ़िक़्ह के सामान्य अध्यायों पर अपनी विशेष शैली में ही किताब लिखेंगे। इसमें जहाँ-जहाँ ‘अहलियत’ का मसला आता जाएगा वहाँ उससे बहस करते जाएँगे। जहाँ वह ‘बुयूअ’ के आदेश बयान करेंगे तो जब यह बयान करेंगे कि कौन व्यक्ति क्रय-विक्रय करने के योग्य है, तो वहाँ बयान करेंगे कि वह आक़िल हो, वयस्क हो, बच्चा हो तो क्या होगा, बच्चों के लिए क्रय-विक्रय के आदेश क्या होंगे। फिर जब निकाह के अध्याय में आएँगे तो जब बच्चों के निकाह की बहस में आएँगे तो तब कहेंगे कि बच्चा अगर ईजाबो-क़ुबूल कर ले तो उसकी क्या हैसियत होगी। इस तरह से वे अलग-अलग अध्यायों में इसपर बहस करते थे। पश्चिमी क़ानूनों और ख़ास तौर पर रोमन लॉ में इन धारणाओं को पहले बयान किया जाता था। पहले धारणाएँ और विचारधाराएँ आती थीं और फिर यह मरहला आता था कि उनको विस्तार पूर्वक किस प्रकार लागू किया जाए। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की शैली इसके विपरीत थी। सम्भवतः यूनानियों की निगनात्मक तार्किकता के प्रभाव से यूरोप में पहले मूल सिद्धान्त और सामान्य धारणाओं और बाद में आंशिक समस्याओं और विस्तृत विवरण से बहस होती थी। इसके विपरीत इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के यहाँ सम्भवत: क़ुरआन-पाठ की शैली प्रभाव के अन्तर्गत आंशिकता ही के सिलसिले में मूल सिद्धान्तों को और आंशिकता ही के पर्दे में उसूल को बयान किया जाता था। यही शैली इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के यहाँ उन्नीसवीं सदी के अन्त तक प्रचलित रही। अब इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बीसवीं सदी में यह किया कि फ़िक़्ह की तमाम किताबों को लेकर उनको खंगाला, इन किताबों में बयान की गई इन धारणाओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उनको संकलित यानी सिस्टमेटाइज़ किया। फिर उनके संकलित सिद्धान्त बनाए और अलग-अलग किताबों के रूप में दुनिया के सामने उनको पेश कर दिया। यह फ़िक़्हे-इस्लामी के मामले में इतना बड़ा और इतने निराले अंदाज़ का काम है जो पिछले तेरह सौ वर्ष में पहली बार हुआ है।
तेरह सौ वर्ष में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जो सोचा, जो लिखा, फ़िक़्हे-इस्लामी के आदेश जिस तरह से संकलित किए, उनके पीछे कार्यरत सामान्य विचारधाराओं और नियमों को क़ानूनी सिद्धान्तों और धारणाओं के शीर्षक से अलग-अलग साइंटिफ़िक अंदाज़ में संकलित करने का काम इस दौर में हुआ है। इसपर अरब दुनिया में एक दो नहीं, बल्कि सैंकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इस असाधारण काम पर अरब दुनिया के फ़ुक़हा हम सबके शुक्रिये के हक़दार हैं। इस शैली पर पाकिस्तान में कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। शरीअत को लागू करने के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे दावे बार-बार होते रहे, लेकिन यह काम जो इन्तिहाई ज़रूरी है और जिसके बिना शरीअत को लागू नहीं किया जा सकता, यह पाकिस्तान में नाम मात्र ही हो सका है।
आज से दस वर्ष पहले हमने अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी में यह तय किया कि विभिन्न इस्लामी विषयों (themes) पर हम सौ मोनोग्राफ़ तैयार करवाएँगे। यह मोनोग्राफ़ जो सौ महत्त्वपूर्ण क़ानूनी धारणाओं पर तैयार किए जाने थे, हमने उसकी सूची बनाई। हर शीर्षक की अलग-अलग रूपरेखा तैयार की, हर रूपरेखा में जो कुछ लिखना चाहिए था उसकी निशानदेही की, फिर हर शीर्षक पर दो-दो, तीन-तीन आधुनिक किताबें जो अरब दुनिया में लिखी गईं, उनकी निशानदेही की और उनको प्राप्त किया। उनकी फ़ोटो कॉपियाँ करवाईं। बड़ी किताबों में जहाँ-जहाँ ये धारणाएँ चर्चा में आई हैं उनकी निशानदेही की और सम्बन्धित पृष्ठों की फ़ोटो कॉपियाँ करवाईं। यों हर शीर्षक पर अलग-अलग फ़ाइल बन गई। इस काम पर कई महीने लग गए। हमारे ज़ेहन में यह था कि यह काम अब इतना आसान हो गया है कि हम पाकिस्तान में बड़ी संख्या में विद्वान लोगों से कहेंगे कि अब काम की यह सारी रूपरेखा तैयार है। साथ ही सामग्री भी मौजूद है। आप इस सामग्री को उर्दू/हिन्दी में इस क्रम से संकलित कर दें। इसको आप मेरा भोलापन कह लें। मुझे यह स्वीकार है कि मैंने यह समझकर नासमझी और बेवक़ूफ़ी की कि यह काम दस बारह महीनों में हो जाएगा। मैं यह समझे बैठा था कि तीन चार महीनों में इस तरह की कोई किताब संकलित कर देना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सामग्री मौजूद है, विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध कर दी गई है, क्रम मौजूद है। दो-तीन महीनों में सब ड्राफ़्ट आ जाएँगे और हम उनको एडिट करके अगले वर्ष सौ किताबें छाप देंगे। मैंने ज़िम्मेदार लोगों से भी कह दिया कि हम अगले वर्ष तक इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाओं पर सौ मोनोग्राफ़ तैयार कर रहे हैं। यह बात 1991 ई॰ की है। 1992 ई॰ में हमने यह सारी योजना तैयार कर ली थी। आज 2004 ई॰ है। अभी तक केवल एक मोनोग्राफ़ छपकर तैयार हो सका है। जिन-जिन लोगों को हमने लिखा उनमें से किसी ने भी यह मोनोग्राफ़ तैयार करके नहीं दिया। मैं शिकायत नहीं करता। लोगों की वाक़ई मजबूरियाँ होंगी, लेकिन यह एक दुखद घटना है कि वादा करने के बावजूद उनमें से किसी एक ने भी काम नहीं किया। पाकिस्तान के माहौल के अनुसार हमने इस काम के लिए बहुत अच्छे मुआवज़े की पेशकश भी की थी। हमारे देश में ज्ञानपरक और दीनी (धार्मिक) काम का स्वभाव नहीं है। लोग लगकर ज्ञानपरक काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उसके कारण पता नहीं क्या हैं, लेकिन जब तक मौलिक, ज्ञानपरक और ज़रूरी शैक्षिक काम नहीं होगा उस समय तक फ़िक़्हे-इस्लामी देश में ज़िन्दा क़ानून के तौर पर जारी नहीं हो सकती। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के काम का उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने पूरी दुनिया में फ़िक़्हे-इस्लामी को ज़िन्दा क़ानून बनाकर दिखा दिया। लेकिन काम कितना किया, आपने क़ुरआन और हदीस पर मेरी चर्चा सुन ली। इससे अनुमान कर लें कि कितना बड़ा काम होने के बाद यह आसानी पैदा हुई। अब बहुत-से लोग यह समझते हैं कि आज वे किसी आन्दोलन का एलान करेंगे और नारा लगाएँगे और अगले दिन से देश में शरीअत लागू हो जाएगी। याद रखिए कि यह समझना मात्र नासमझी है। यह इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ लोग अपनी जीवनियाँ इस काम के लिए क़ुर्बान करें। न किसी बदले की तमन्ना करें, न तारीफ़ की परवाह करें और ख़ामोशी से ऐसा काम कर जाएँ कि उनके मरने के बाद ही दुनिया को पता चले कि कितना काम हुआ था, जिससे लोग फ़ायदा उठाएँगे। यह जो मैंने ज़िक्र किया था कि इस्लामी बैंकिंग पर इतना काम हुआ है, इतने लोग इसमें शामिल हैं कि जिनके नाम भी कोई नहीं जानता। कुछ लोग जानते हैं कि कितनी सख़्त मेहनत और सूक्षम दृष्टि से और कितने लम्बे समय में यह काम हुआ है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते।
इस लम्बे और कठिन मेहनत से किए गए काम के बाद अब यह मरहला आ गया है कि कई देशों के स्टेट बैंकों ने लीगल फ़्रेमवर्क जारी कर दिए हैं और अब दुनिया-भर के मुस्लिम देशों के स्टेट बैंक मिलकर मुस्लिम जगत् के लिए एक नया फ़्रेमवर्क जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे काम की तैयारी करने में पचास वर्ष का समय लगा है। शेष कामों में भी इतना ही समय लगेगा। इस तरह के काम तीन मैदानों में बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। एक फ़ौजदारी क़ानूनों के मैदान में, दूसरा व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के मैदान में, और तीसरा संवैधानिक धारणाओं के मैदान में। इस्लामी संवैधानिक धारणाओं पर बीसवीं शताब्दी में अत्यन्त उल्लेखनीय काम हुआ है। सैंकड़ों, बल्कि हज़ारों की संख्या में विद्वानों ने इस काम में हिस्सा लिया और इस्लाम के दृष्टिकोण को पूरी तरह स्पष्ट करके रख दिया। इस्लाम की संवैधानिक धारणाएँ क्या हैं, अब इस बारे में मुस्लिम जगत् के अन्दर कोई उल्लेखनीय मतभेद नहीं है। आंशिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस विषय पर मूल सिद्धान्तों और महत्त्वपूर्ण धारणाओं में Clarity (स्पषटता) पैदा हो चुकी है परस्पर सहमति मौजूद है और यह मालूम है कि अब इस दौर में अगर इस्लामी राज्य बनेगा तो किन दिशानिर्देशों पर बनेगा और उसका संविधान तैयार हो तो किन दिशानिर्देशों पर होना चाहिए।
बातें तो और भी बहुत-सी हैं, लेकिन समय बहुत हो गया। सवालात भी आज शायद ज़्यादा हों, इसलिए शेष चर्चा छोड़ देता हूँ।
सवालात
सवाल : जहाँ तक मुझे यह बात समझ मेँ आई वह यह है कि इनसान को ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए अवश्य ही किसी-न-किसी मसलक को अपनाना पड़ता है। क्या यह दुरुस्त है? अगर नहीं, तो फिर सही क्या है? आख़िर इन मसलकों के माननेवाले एक-दूसरे के दुश्मन क्यों हैं?
जवाब : मैं यह नहीं मानता कि मसलकों के चाहनेवाले एक-दूसरे के दुश्मन हैं। मेरी तो किसी मालिकी या शाफ़िई या हंबली से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ और यही देखता हूँ कि सभी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई शाफ़िई आलिम पाकिस्तान आया हो और लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार न किया हो। या कोई मालिकी विद्वान हमारे यहाँ आया हो और उसको मस्जिद में घुसने न दिया गया हो। हमारे यहाँ फ़ैसल मस्जिद में हर जुमा को नया ख़तीब नमाज़ पढ़ाता है। कभी कोई शाफ़िई होता है, कभी हंबली होता है और कभी मालिकी या हनफ़ी। वहाँ हर जुमा को कम-से-कम बीस-पच्चीस हज़ार नमाज़ी एक नए इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और कोई शिकायत पैदा नहीं होती। मेरे ख़याल में मसलकों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है और अगर दुश्मनी है तो जाहिलों में होगी। इस दुश्मनी का हल यह है कि जहालत दूर करके इल्म को फैलाया जाए।
कल भी किसी ने इस प्रकार का सवाल किया था। मैंने कहा था कि जो अब तक करते आ रहे हैं वही जारी रखें। अगर अब तक आपका कोई मसलक नहीं था तो उसी तरह चलें और अगर अब तक कोई मसलक था तो अब भी उसी के अनुसार अमल जारी रखें। और अगर मसलक छोड़ना हो तो पहले इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि आपको पता चल जाए कि अब तक आप जिस मसलक का पालन कर रहे थे, उसके तर्क क्या हैं और जिस मसलक को उपनाना चाहते हैं, उसके तर्क क्या हैं। जब इस हद तक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर जिस तरह का फ़ैसला करना हो कर लें।
✩
सवाल : एक बहन ने दुआ की है कि आपने बहुत आसान और स्पष्ट करके मुश्किल विषय बयान किए। अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे, आमीन!
Is there any institute which is teaching accounting and auditing according to Islamic point of view or are there any organizations which are practising Islamic accountcancy?
[क्या कोई ऐसा संस्थान है जो इस्लामी दृष्टिकोण के अनुसार लेखांकन और लेखा परीक्षा सिखा रहा है या क्या कोई ऐसा संगठन है जो इस्लामी लेखाशास्त्र का अभ्यास कर रहा है?]
जवाब : अभी तक तो कोई ऐसी संस्था मेरी जानकारी की हद तक मौजूद नहीं है जिसमें इस्लामिक अकाउंटेंसी का प्रशिक्षण होता हो। लेकिन इस्लामिक अकाउंटेंसी की दस्तावेज़ात आयोफ़ी नामक संस्था ने, जिसके बारे में मैंने बताया, उन्होंने तैयार की हैं। हमारे यहाँ इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमने कुछ कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं जिनको हम जल्द ही लॉन्च करनेवाले हैं। उनमें चार हफ़्ते के कोर्स भी हैं, दो हफ़्ते के और शॉर्ट टर्म (अल्पावधि) के कोर्स भी हैं जो विभिन्न स्तर के बैंकर्ज़ और दूसरे लोगों के लिए जारी किए जाएँगे। अकाउंटेंसी के कुछ कोर्स दुनिया में होते हैं। कुछ क़तर में होते हैं। इंगलैंड में भी इस्लामी बैंकिंग की एक संस्था है जिसके प्रमुख मुअज़्ज़म अली साहब हैं। वहाँ भी यह कोर्स होता है। अभी हमने मुअज़्ज़म अली साहब की संस्था से एक अनुबन्ध किया है। जिसके तहत हम उनके सहयोग से अकाउंटिंग के कुछ कोर्स करेंगे। अकाउंटिंग के कोर्सों में हमें मूल रूप से दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक फ़िक़्ह के मौलिक आदेश और शरीअत का महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन, जो आधुनिक कारोबार के लिए अपरिहार्य हैं। दूसरे अकाउंटेंसी के वे तरीक़े जो इस्लामी संस्थाओं की अकाउंटेंसी के लिए अपरिहार्य हैं।
इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमने एक प्रोग्राम एमएससी और इस्लामिक बैंकिंग और फ़ाइनांस में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू किया है। इसमें इस्लामिक अकाउंटेंसी पर भी एक कोर्स है, जो लोग डिप्लोमा करना चाहें वे दस महीनों में डिप्लोमा कर सकते हैं और जो एमएससी करना चाहते हैं वे डिप्लोमा के बाद एक वर्ष और लगाकर एमएससी कर सकते हैं। यह प्रोग्राम बहुत सफल है। शाम को होता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं। शाम से लेकर रात नौ बजे तक इसकी क्लासें होती हैं। अब तक इस में तीन बैच काम कर रहे हैं। एक पास आउट हो चुका है।
✩
सवाल : Kindly tell us about the language in which these monographs are prepared? [कृपया हमें बताएँ कि ये मोनोग्राफ किस भाषा में तैयार किए गए हैं?]
जवाब : अभी कहाँ तैयार हो गए हैं। हम तो उर्दू में करना चाहते थे। केवल एक ही हुआ है। उर्दू में एक तैयार हुआ है, आप चाहें तो इस्लामी यूनिवर्सिटी की शरीआ अकैडमी से ले लें।
✩
सवाल : Sir you told us about masters in this subject. I am interested do it. Would you provide me further information? [सर, आपने हमें इस विषय में मास्टर्स के बारे में बताया। मुझे इसमें रुचि है। क्या आप मुझे और जानकारी देंगे?]
जवाब : अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक कुल्लियतुश-शरीआ है। जहाँ एलएलबी (आनर्स) शरीआ ऐंड लॉ, एलएलबी शरीआ, बीए आनर्स शरीआ और इस तरह के कई कोर्स होते हैं। ये तीन से चार वर्ष तक या पाँच साल तक की अवधि में होते हैं। फिर एलएलएम इस्लामिक लॉ, अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून, इंटरनेशनल ट्रेड और कॉर्पोरेट फ़ाइनांसिंग में होता है। इन सबमें शरीआ लॉ एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इन सबमें जो इस्लामिक लीगल कंटेंट है वह अनिवार्य है। अब हम इस्लामी उसूले-फ़िक़्ह में भी अगले वर्ष से एलएलएम शुरू करवा रहे हैं। आप चाहें तो आ जाएँ।
✩
सवाल : कृपा करके इंशोरेंस पर कोई लेक्चर ज़रूर दें। मेरे घरवालों ने मेरे नाम पर बहुत बड़ी रक़म की इंशोरेंस कराई है। अब उसकी एक ही क़िस्त जमा कराई है। मैं बहुत कहता हूँ कि यह जायज़ नहीं। लेकिन घरवाले नहीं मानते और कहते हैं कि ज़माने के साथ चलना पड़ता है। बताइए मैं क्या करूँ। क्या इस रक़म को हदिया या सदक़ा करना दुरुस्त है या घरवालों को उनकी मर्ज़ी करने दूँ?
जवाब : यह आप मुझे अलग से लिखकर बताएँ कि आपके घरवालों ने कहाँ और किस संस्था में इंशोरेंस की रक़म जमा करवाई है और इस संस्था की इंशोरेंस का विवरण क्या है। उसको देखकर ही में कुछ बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। इंशोरेंस के कुछ प्रकार जायज़ हैं। कुछ नाजायज़ हैं और कुछ को मजबूरी में अपनाया जा सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है। उदाहरण के रूप में री-इंशोरेंस है। इसकी जितनी संस्थाएँ हैं वे सब पाकिस्तान से बाहर हैं। किसी मुस्लिम देश में री-इंशोरेंस की संस्था नहीं है। री-इंशोरेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। उदाहरण के रूप में जितने हवाई जहाज़ वातावरण में उड़ रहे हैं उनकी री-इंशोरेंस ज़रूरी है। कोई एयर लाइन उस समय तक काम नहीं कर सकती जब तक वह अपने जहाज़ों की री-इंशोरेंस न कराए। ऐसी स्थिति में या तो आप री-इंशोरेंस कराएँ या फिर पीआईए को बंद कर दें। दो ही शक्लें हैं। इसलिए पीआईए को मजबूरन री-इंशोरेंस करवानी पड़ती है। यह इतनी बड़ी रक़म का मामला है कि कोई मुस्लिम देश अभी तक री-इंशोरेंस कम्पनी क़ायम ही नहीं कर सका है। प्रस्ताव आते रहते हैं कि सारे मुस्लिम देशों को मिलकर एक बड़ी री-इंशोरेंस कम्पनी बनानी चाहिए। जितने समुद्री जहाज़ हैं वे री-इंशोरेंस होते हैं। तो यह वाक़ई ऐसी स्थिति है जहाँ वाक़ई मजबूरी होती है।
सवाल : शीया लोगों के बारे में कुछ लोगों कहते हैं कि ये काफ़िर और मुनाफ़िक़ीन हैं। शीया हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त को नहीं मानते और इसकी दलील यह देते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ख़िलाफ़त के जो गुण दे गए हैं वे इन लोगों में मौजूद नहीं थे, कुछ लोगों का कहना है कि संविधान में उनको काफ़िर लिखवाना है।
जवाब : देखिए ये बड़ी ग़ैर-ज़िम्मेदारी की बातें हैं। जो लोग ये बातें कहते हैं सर्वोच्च अल्लाह उनको हिदायत दे। उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिएँ। यह मुस्लिम जगत् में एक टाइम बम रखने के समान है। शीया लोग आज से नहीं हैं। कम-से-कम तेरह सौ वर्ष से चले आ रहे हैं। कभी भी मुसलमानों ने उनको काफ़िर नहीं कहा। बड़े-बड़े विद्वानों ने शीया अक़ीदों (धार्मिक अवधारणाओं) का अध्ययन किया तो उन्हें ग़लत तो कहा, उनकी आलोचना भी की और उनकी कमज़ोरियाँ भी स्पष्ट कीं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि शीया इस्लाम के दायरे से बाहर हैं। अत: यह बात जो पिछले पंद्रह-बीस वर्षों से पैदा हुई है, उसने मुस्लिम जगत् में बड़ा बिगाड़ पैदा किया है। मेरे नज़दीक शीयों के अक़ीदे ग़लत हैं। इस्लाम के अनुसार नहीं हैं। बस बात समाप्त हो गई। मैं उनके अक़ीदों को सही नहीं समझता। लेकिन ग़लत अक़ीदों के ध्वजावाहक अतीत में बहुत-से लोग रहे हैं। ख़वारिज के बहुत-से अक़ीदे ग़लत थे। लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं कहा कि वे इस्लाम से ख़ारिज हैं। शीया उस समय भी मौजूद थे। हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त का इनकार करनेवाले, और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) की ख़िलाफ़त का इनकार करनेवाले पहली सदी में भी बहुत थे। लेकिन किसी ने उनको काफ़िर नहीं कहा। किसी की ख़िलाफ़त के इनकार से कोई काफ़िर नहीं होता। जिस चीज़ के इनकार से आदमी काफ़िर होता है वह क़ुरआन और सुन्नत हैं। पवित्र क़ुरआन में कहीं भी नहीं आया कि ऐ मुसलमानो! अबू-बक्र और उमर को ख़लीफ़ा मानो। जो शख़्स इन बड़े और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की ख़िलाफ़त का इनकार करता है वह एक सच्चाई का इनकार करता है। अगर कोई इनकार करे कि सूरज नहीं निकला तो वह एक सच्चाई का ‘इनकारी’ होगा। सच्चाई के इनकार से कोई व्यक्ति काफ़िर नहीं हो जाएगा। उसकी बेवक़ूफ़ी अपनी जगह। बेवक़ूफ़ होना अलग बात है और काफ़िर होना अलग बात है। इस तरह जाहिल होना अलग बात है और काफ़िर होना अलग बात।
☆
सवाल : क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम ब्याज-मुक्त हो जाएगा।
जवाब : मुझे विश्वास है कि जो प्रस्ताव अब आ रहे हैं और जो नया लीगल फ़्रेमवर्क स्टेट बैंक ने जारी किया है, उससे ब्याज रहित बैंकिंग की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी और देश में एक नई आधारशिला पड़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप इस्लामी व्यापार और कारोबार का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन इसका दारोमदार केवल स्टेट बैंक या किसी और संस्था पर नहीं है। बल्कि उसका अस्ल दारोमदार कारोबारी और व्यापारी वर्ग पर है।
मुझे कई वर्ष पहले स्यालकोट के चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने बुलाया था कि मैं वहाँ ब्याज रहित बैंकिंग पर लैक्चर दूँ। बहुत पहले की बात है। मैंने उनसे कहा कि मैं बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से वह बात सुनेंगे। वह यह है कि ब्याज रहित कारोबार इस देश में बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है। हमारे देश में ब्याज रहित बैंकिंग उतनी ही आसान है कि जिस तरह एक स्विच ऑन करने से पूरा कमरा रोशन हो जाता है, इसी तरह एक स्विच ऑन करने से ब्याज रहित कारोबार देश में शुरू हो सकता है। इसी तरह यह काम इतना मुश्किल है जैसे किसी जंगल में बिजली का कोई प्रबन्ध ही न हो और आप स्विच ऑन करके बल्ब रौशन करना चाहें तो यह कभी नहीं हो सकता।
आसान रास्ता और आसान समाधान तो यह है कि आज ही तमाम व्यापारी तय कर लें कि वे केवल ब्याज रहित कारोबार करेंगे। जिस लम्हे वे यह तय कर लेंगे उसी लम्हे देश में ब्याज रहित कारोबार शुरू हो जाएगा। मैं निजी तौर पर ऐसे व्यापारियों को जानता हूँ। एक दो नहीं दर्जनों को जानता हूँ जिन्होंने जीवन में कभी एक पैसा का ब्याज भी नहीं लिया और न ही एक पैसा कभी बैंक में रखा है। लेकिन उनका करोड़ों का कारोबार है। मैंने स्वयं जाकर उनके कारोबार देखे हैं। उनसे मिला हूँ। उन लोगों का काम देखकर विश्वास पुख़्ता हो जाता है कि कारोबार के लिए ब्याज अपरिहार्य नहीं है। अगर आज राजा बाज़ार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सारे व्यापारी तय करें कि हम ब्याज नहीं लेंगे, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ब्याज समाप्त हो जाएगा। आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत-से व्यापारी न ब्याज लेते हैं और न देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके कारोबार चल रहे हैं। तो यह समझना कि ब्याज के बिना कारोबार नहीं चल सकता यह ग़लत बात है। ठीक है, एक सतह तक कारोबार में दिक़्क़त होती है। लेकिन इस सतह से नीचे के कारोबार सौ प्रतिशत ब्याज के बिना चल सकते
हैं।
इसमें अस्ल ज़िम्मेदारी और फ़ैसला करना व्यापारियों का है। मान लीजिए, कल हुकूमत क़ानून बना दे और व्यापारी उसकी परवाह न करें तो जो हश्र शेष क़ानूनों का हुआ है इस तरह का हश्र इस क़ानून का भी होगा। अगर दो व्यापारी चुपके से आपस में ब्याज आधारित लेन-देन कर लें और यह लेन-देन क़ानून के अनुसार नाजायज़ हो तो क़ानून क्या कर लेगा। जैसे शेष क़ानूनों की दुर्गति हो रही है इसी तरह इसकी भी होगी।
—:☆:—
Recent posts
-

मुसलमानों का अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह एक विश्लेषण (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 11)
17 April 2025 -

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025