
मुसलमानों का अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह एक विश्लेषण (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 11)
-
फ़िक़्ह
- at 17 April 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक: गुलज़ार सहराई
लेक्चर नम्बर-11 (11 November 2004)
पिछले दस दिनों की चर्चा में फ़िक़्हे-इस्लामी का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया। इसके मौलिक विषयों की निशानदेही की गई और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं और विभागों की मौलिक धारणाओं, सिद्धान्तों एवं लक्ष्यों का उल्लेख किया गया। पिछले दस दिनों में फ़िक़्हे-इस्लामी की व्यापकता, गहराई और सारगर्भिता का किसी-न-किसी हद तक अनुमान हो गया होगा। आज की चर्चा में मुसलमानों के अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह का एक सरसरी जायज़ा पेश करना अभीष्ट है। इस अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह के सामान्य विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि एक नज़र में इस बात का अनुमान हो जाए कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने पहली सदी हिजरी से लेकर आज तक जो विस्तृत फ़िक़ही साहित्य तैयार किया है, उसकी सीमाएँ क्या हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। कितनी असाधारण और ज्ञानवर्द्धक किताबें इस भंडार में मौजूद हैं। इससे लाभान्वित होने का आम तरीक़ा और शैली क्या है। ये किताबें जो हज़ारों से बढ़कर लाखों की संख्या में हैं, इनकी तैयारी में मानवजाति के बेहतरीन दिमाग़ों ने हिस्सा लिया है। उनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने अतीत से जुड़ी न हो, वर्तमान की समस्याओं का प्रत्यक्ष जवाब न देती हो और भविष्य के लिए आधार उपलब्ध न करती हो। उनमें से कोई काम अन्तरिक्ष में नहीं हुआ। यह सारा काम एक क्रमबद्ध प्रोग्राम का एक हिस्सा है। वह क्रमबद्ध प्रोग्राम जिसकी जड़ें पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल में हैं। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस्लामी शरीअत की उन मौलिक धारणाओं से है जिनपर मुसलमानों का आम तौर पर मतैक्य रहा है।
फ़िक़्हे-इस्लामी की विविधता और व्यापकता
यह फ़िक़ही संग्रह विभिन्न फ़िक़्ही मसलकों के इस्लामी विद्वानों ने अलग-अलग भी तैयार किया है। और इसमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जो समष्टीय रूप से फ़िक़्हे-इस्लामी से बहस करती हैं। जिनका किसी ख़ास फ़िक़ही मसलक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। यों तो हममें से हर एक को यह बात याद रखनी चाहिए कि फ़िक़्हे-इस्लामी का यह सारा संग्रह मुसलमानों का संग्रह है। फ़िक़्हे-इस्लामी की ये सारी किताबें मुसलमानों की किताबें हैं। इन सब किताबों की तैयारी में इन इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने हिस्सा लिया है जो हर मुसलमान के हार्दिक सम्मान के पात्र हैं। अत: इस महत्वपूर्ण ज्ञानपरक काम को फ़िक़ही सीमाओं में सीमित नहीं कर देना चाहिए। इस वैचारिक समुद्र को फ़िक़्ही मसलकों की संकीर्णताओं में सीमित कर देना इसकी व्यापकता और सार्वभौमिकता को झुठलाने के समान है। यह कहना कि अमुक किताब का सम्बन्ध मेरे फ़िक़ही मसलक से है, इसलिए मुझे उसका भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए, और अमुक किताब का सम्बन्ध मेरे फ़िक़ही मसलक से नहीं है, इसलिए मुझे उपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, यह एक बहुत बड़े अभागेपन की बात है।
यह मात्र एक प्रशासनकि सुविधा या निहितार्थ की बात है कि किसी ख़ास इलाक़े के लोग किसी ख़ास इज्तिहाद की पैरवी करने लगे हैं। किसी ख़ास इलाक़े में कुछ ख़ास फ़ुक़हा की किताबें ज़्यादा प्रचलित हो गईं। ऐसा मात्र कुछ प्रशासनकि सुविधाओं के कारण हुआ है। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि उदाहरणार्थ इमाम मालिक (रह॰) और उनके इज्तिहाद की शैली की पैरवी करनेवाले फ़ुक़हा ने जो फ़िक़ही संग्रह तैयार किया है, वह भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का फ़िक़ही संग्रह नहीं है। या मावराउन्नहर के इस्लामी विद्वानों के फ़िक़ही इज्तिहादात और फ़तवों से मिस्र और सीरिया के आलिमों को लाभान्वित नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि यह सारी साझा पूँजी फ़िक़्हे-इस्लामी की पूँजी है और इस दृष्टि से यह मुस्लिम समाज की एक साझी विरासत है। इस साझी विरासत की जानकारी दो कारणों से ज़रूरी है।
एक वजह तो यह है कि इस्लाम से अनजान वर्तमानकाल के मुसलमानों को यह अनुमान हो जाए कि फ़िक़्हे-इस्लामी की व्यापकता क्या है। इसकी dimensions क्या हैं और कैसे-कैसे बड़े इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसकी तैयारी में हिस्सा लिया है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आगामी दिनों में और आनेवाली सदियों में फ़िक़्हे-इस्लामी का यह पूरा संग्रह मुसलमानों के लिए एक नई व्यवस्था का आधार बनेगा। आगे जो व्यवस्था आनेवाली है, उसका आधार किसी निर्धारित फ़िक़ही मसलक पर नहीं होगा, बल्कि उसका आधार फ़िक़्हे-इस्लामी के पूरे-के-पूरे संग्रह पर होगा।
एक कॉस्मोपॉलिटन फ़िक़्ह का गठन
इस बात को और भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है। आधुनिक काल में इस्लाम की राजनैतिक व्यवस्था के बारे में चिन्तन-मनन हो रहा है। इस्लाम की संवैधानिक सोच पर किताबें लिखी जा रही हैं। विभिन्न मुस्लिम देशों में संवैधानिक धारणाओं पर चर्चाएँ हो रही हैं। और ऐसी दस्तावेज़ात और तहक़ीक़ात सामने आ रही हैं जिनका उद्देश्य इस दौर की अपेक्षाओं को सामने रखते हुए, इस्लाम के संवैधानिक सिद्धान्तों और राजनैतिक धारणाओं के आधार पर एक नई संवैधानिक और राजनैतिक व्यवस्था का गठन है। यह काम पाकिस्तान में भी हो रहा है। मिस्र और दूसरे अरब देशों में भी हो रहा है।
उनमें से किसी काम को हनफ़ी या शाफ़िई या हंबली या मालिकी मसलक की सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता। इस समय मुस्लिम जगत् में इस्लामी संविधान बनाने का काम हो रहा है। हनफ़ी संविधान बनाने या मालिकी और हंबली संविधान बनाने का काम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में अगर इस्लामी संविधान की तरफ़ पहल की गई है तो वह इस्लामी संविधान की तरफ़ पहल हुई है, किसी हनफ़ी या मालिकी संविधान की तरफ़ पहल नहीं हुई है। इसी तरह से मुस्लिम जगत् में नए व्यापारिक, आर्थिक और कारोबारी उद्देश्य के लिए आधुनिक शैली के अनुसार क़ानून तैयार किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि पाकिस्तान में ब्याज रहित बैंकिंग के मामले में ख़ासा काम हुआ है। अनेक इस्लामी बैंक क़ायम हो रहे हैं। विभिन्न बैंकों ने इस्लामी बैंकिंग के लिए अपने यहाँ उप विभाग क़ायम किए हैं या क़ायम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। यह काम दुनिया के हर मुस्लिम देश में हो रहा है। यहाँ तक कि ग़ैर-मुस्लिम देशों में भी ब्रिटेन, फ़्रांस, हाँगकांग और कई दूसरे देशों में इस्लामी बैंकिंग की संस्थाएँ अस्तित्व में आ रही हैं और वहाँ के मुसलमान विद्वान, क़ानून एवं शरीअत के विशेषज्ञ इस्लामी बैंकिंग के नियम-क़ानून तैयार कर रहे हैं।
ये सारे क़ायदे-क़ानून जो दुनिया-भर में तैयार हो रहे हैं, इन सबमें एक-दूसरे से लाभ उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में होनेवाले काम के प्रभाव मिस्र और सऊदी अरब में पड़ रहे हैं। मिस्र और सऊदी अरब में जो शोध हो रहा है उससे पाकिस्तान लाभान्वित हो रहा है। इसलिए यह सारा काम एक साझी परिकल्पना और साझे मूल्यों और सिद्धान्तों के आधार पर किया जा रहा है। उनमें किसी निर्धारित फ़िक़ही मसलक का पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाँचे ईरान में ब्याज रहित बैंकिंग का जितना काम हुआ है, वह सारे-का-सारा क़रीब-क़रीब उसी अंदाज़ का है जिस अंदाज़ का पाकिस्तान में हुआ है। इसलिए कि ये वे समस्याएँ हैं जिनमें किसी फ़िक़ही मतभेद की गुंजाइश बहुत कम है। जो चीज़ें शरीअत में हराम हैं वे सबके नज़दीक हराम हैं। ‘रिबा’, ‘ग़रर’, ‘क़िमार’ सबके नज़दीक हराम हैं। शरीअत की सीमाओं के अन्दर कारोबार की जो जायज़ शक्लें हैं, वे लगभग एक जैसी हैं। इसलिए फ़िक़्हे-इस्लामी का यह नया विकास और यह नया रुझान मसलकी नहीं, बल्कि मसलकी सीमाओं से परे है। इसलिए आगे आनेवाले साल, दशक या शताब्दी मसलकों की शताब्दी नहीं होगी, बल्कि यह फ़िक़्हे-इस्लामी की साझी शताब्दी होगी। इसलिए आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि फ़िक़्हे-इस्लामी के छात्र फ़िक़ही संग्रहों से अवगत हों। कम-से-कम अध्ययन और जानकारी की हद तक एक निर्धारित मसलक में सीमित न रहें। उनको इज्तिहाद की तमाम फ़िक़ही शैलियों की जानकारी होनी चाहिए। वे यह जानते हों कि फ़िक़्हे-मालिकी की मौलिक धारणाएँ और नियम क्या हैं। फ़िक़्ह हंबली और दूसरे महत्वपूर्ण फ़िक़ही मसलकों और इज्तिहादात की मौलिक धारणाएँ और नियम क्या हैं।
जब तक यह आधार ज्ञानपरक दृष्टि से मज़बूत नहीं होगा, उस समय तक आगे आनेवाली शताब्दी या आगे आनेवाले दशकों में इस काम को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा।
इन दो कारणों से यह बात अत्यन्त उचित बल्कि ज़रूरी है कि फ़िक़्हे-इस्लामी के छात्रों की नज़र मुसलमानों के अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह और इस्लामी शरीअत की तफ़सीर एवं व्याख्या की इस साझी विरासत पर रहे जो समष्टीय रूप से विभिन्न फ़िक़ही मसलकों के मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा और मुफ़्तियों ने तैयार किया है। यह फ़िक़ही संग्रह विभिन्न अंदाज़ और मोटाई की हज़ारों, बल्कि शायद लाखों किताबों पर आधारित है। यह बहुत-सी किताबों पर फैला हुआ है। ये तमाम किताबें बारह सौ वर्ष के लम्बे समय में लिखी गई हैं। इनमें दर्जात और महत्व की दृष्टि से अन्तर पाया जाता है और सबका दर्जा एक नहीं है। उनको विभिन्न वर्गों या दर्जों में विभक्त किया गया है।
उम्महाते-मज़हब
सबसे पहला दर्जा उन मौलिक किताबों का है जिनको हम ‘उम्हाते-मज़हब’ या ‘धार्मिक सिद्धान्त’ कहते हैं। यहाँ ‘मज़हब’ से मुराद religion नहीं है, बल्कि इससे मुराद फ़िक़ही मसलक (पन्थ) है। यानी किसी फ़िक़ही मसलक की वे मौलिक और सर्वप्रथम किताबें जिनपर इस मसलक का दारोमदार है। ये किताबें तमाम फ़िक़ही मसलकों में पाई जाती हैं। जो फ़िक़ही मसलक आज शेष रह गए हैं, वे इसी लिए शेष रह गए हैं कि उनके संकलनकर्ताओं ने अपने विचारों और इज्तिहादात को किताबों के रूप में संकलित कर दिया था और उन मुज्तहिदीन के इज्तिहादात, उनकी तर्क देने की शैली, सब कुछ एक ज्ञानपरक और साइंटिफ़िक रूप में दुनिया के सामने आ गया था। जो फ़िक़ही मसलक ज़्यादा समय तक शेष न रह सके और समय के साथ-साथ मिट गए, उनके मिट जाने के बहुत-से कारणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उनके संकलनकर्ताओं ने अपने विचारों और इज्तिहादात, अपने तर्कों के परिणामों को किताबी रूप में संकलित नहीं किया था, इसलिए बाद में आनेवाले उनके विचारों से लाभान्वित न हो सके।
मुतून (Texts) या मूल पाठ
मूल किताबों के बाद दूसरे दर्जे में जो किताबें शामिल हैं वे ‘मुतून’ कहलाती हैं। ‘मत्न’ का शाब्दिक अर्थ तो किसी चीज़ का अत्यन्त मज़बूत और पायदार हिस्सा है, लेकिन शब्दावली में इससे अभिप्रेत है किसी किताब की अस्ल और मौलिक इबारत। इस्लामी ज्ञान के सन्दर्भ में ‘मत्न’ से अभिप्रेत है किसी कला, ख़ास तौर पर फ़िक़्ह नह्व, कलाम वग़ैरा की वह संक्षिप्त किताब जिसमें उसकी महत्वपूर्ण और मौलिक समस्याओं को आसान लेकिन व्यापक ढंग से बयान किया गया हो। ‘मुतून’ उसका बहुवचन है। मुसलमानों में ‘मुतून’ की तैयारी का काम तीसरी सदी हिजरी में शुरू हुआ। और आइन्दा कई सौ वर्ष तक यह काम जारी रहा। यह ‘मुतून’ फ़िक़्ह में भी तैयार हुए। दूसरे ज्ञान में भी तैयार हुए। और फिर होते-होते मुसलमानों के तमाम ज्ञान-विज्ञान में ऐसे ‘मत्न’ तैयार हुए जो मूल रूप से पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य से लिखे गए थे।
पहली सदी हिजरी से तीसरी सदी हिजरी तक का ज़माना इस्लामी ज्ञान-विज्ञान का आरम्भिक दौर है। ये सारे ज्ञान-विज्ञान एक ज्ञानपरक ढंग से संकलित किए जा रहे थे। तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूले-फ़िक़्ह और शेष ज्ञान-विज्ञान का मूल गठन आरम्भिक तीन सदियों में ही हुआ। जब गठन के दौर का यह मरहला गुज़र गया और एक आधार उपलब्ध हो गया तो यह ज्ञान-विज्ञान इतने फैल गए कि एक विद्यार्थी के लिए मुश्किल हो गया कि इस पूरे भंडार को अपनी पकड़ में लाए। उस समय कुछ लोगों ने महसूस किया कि अगर इस सारे ज्ञान-संग्रह को एक संक्षिप्त टेक्स्ट के अन्दर समो दिया जाए तो छात्रों के लिए समझना भी आसान होगा और याद करना और याद रखना भी आसान होगा। इस दर्सी आवश्यकता की ख़ातिर कुछ ‘मुतून’ लिखे गए। उनमें कोशिश की गई कि इस ज्ञान में इस समय तक जितनी व्यापकता पैदा हुई है, इस सबका अवलोकन करके, उसकी जो मौलिक समस्याएँ हैं और जिनपर इस ज्ञान के विशेषज्ञों का मतैक्य है, उनको एक आसान, संक्षिप्त और व्यापक ‘मत्न’ में समो दिया जाए। यानी ऐसा precise और concise टेक्स्ट तैयार किया जाए जिसको अगर छात्र याद कर लें तो इस ज्ञान की महत्वपूर्ण समस्याएँ उनकी पकड़ में आ जाएँ। इस ग़रज़ के लिए ‘मुतून’ तैयार किए गए। ये ‘मुतून’ फ़िक़्हे-हनफ़ी, शाफ़िई, हंबली, मालिकी, तमाम फ़िक़्हों में तैयार हुए। और बहुत जल्द छात्रों की पाठ्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गए। शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया। छात्रों ने उनको याद करना शुरू किया। इसका परिणाम यह निकला कि विद्यार्थियों के ज़ेहन में सम्बन्धित कला की जड़ आ गई। इस कला की मौलिक समस्याएँ उसकी पकड़ में आ गईं। और आगे से इस कला का विवरण या अन्य शोधपरक मामलों को समझना उसके लिए आसान हो गया। अत: फ़िक़ही किताबों में दूसरा दर्जा ‘मुतून’ का है।
फिर जैसे-जैसे ‘मुतून’ बढ़ते गए और उनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई तो ‘मुतून’ की तैयारी में एक-दूसरे से एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। उदाहरणार्थ आपने एक ‘मत्न’ लिखा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इससे अच्छा ‘मत्न’ लिखूँ। यानी जो समस्याएँ आपसे रह गई हैं मैं वे भी शामिल कर दूँ। जहाँ आपने ग़ैर-ज़रूरी विवरण दिया है उसके मुक़ाबले में मैं बात संक्षिप्त कर दूँ। मैंने एक और ‘मत्न’ तैयार किया। इस दौरान कई और समस्याएँ पेश आईं और नए इज्तिहादात हुए। बाद में आनेवालों ने एक और ‘मत्न’ तैयार किया। इस तरह से ‘मुतून’ की संख्या में वृद्धि होती चली गई। कुछ ‘मुतून’ में ऐसी विशेषताएँ थीं जो दूसरों में नहीं थीं। कुछ लोगों ने चाहा कि वे ऐसे ‘मत्न’ तैयार करें जो पूर्व ‘मुतून’ की विभिन्न विशेषताएँ को एक जगह जमा कर लें।
इन कारणों के आधार पर तमाम ज्ञान-विज्ञान में आम तौर से और फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह में विशेषकर ‘मुतून’ की संख्या में वृद्धि होती चली गई। फिर एक ऐसा ज़माना आ गया कि ‘मुतून’ बहुत मुश्किल होते चले गए और मुश्किल-पसंदी उनकी विशेषता बन गई। इन परिस्थितियों में आवश्यकता पेश आई कि ‘मुतून’ की शरहें (व्याख्याएँ) यानी commentaries तैयार की जाएँ। इस तरह बड़े पैमाने पर ऐसी शरहें तैयार हुईं जिनका उद्देश्य किसी ख़ास ‘मत्न’ के अर्थों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण था।
शरहें (व्याख्याएँ)
फ़िक़्ह की किताबों के संग्रहों में तीसरा दर्जा उन व्याख्याओं का है जो ‘मुस्तनद’ (प्रमाणित) ‘मुतून’ के लिए लिखी गईं। ‘मुस्तनद’ के शब्द को याद रखें। कुछ ‘मुतून’ मुस्तनद थे और कुछ ग़ैर-मुस्तनद (अप्रमाणित) थे। ग़ैर-मुस्तनद ‘मुतून’ लोकप्रिय नहीं हुए। वे आज नहीं पाए जाते। उनमें से कुछ पुस्तकालयों में मख़तूतात (हस्तलेखों) के रूप में मौजूद होंगे। लेकिन व्यवहारतः समाप्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत-से ग़ैर-मुस्तनद ‘मुतून’ लिखे गए थे जो बाद में लोकप्रिय न हो सके और समय गुज़रने के साथ-साथ समाप्त हो गए, क्योंकि या तो लिखनेवालों का ज्ञानपरक दर्जा इतना बुलंद नहीं था। या लिखनेवाले से ऐसी गलतियाँ हो गईं कि इस कला के विशेषज्ञों ने इस ‘मत्न’ को पसंद नहीं किया। इसलिए वे ‘मुतून’ लोकप्रिय नहीं हुए और विश्वसनीय भी क़रार नहीं पाए। जो विश्वसनीय और लोकप्रिय ‘मुतून’ हैं उनकी व्याख्याएँ भी विश्वसनीय और लोकप्रिय हैं।
शरहों (व्याख्याओं) के ज़माने के बाद एक दौर आया जिसमें फ़िक़्ह में बड़ी तेज़ी से व्यापकता आई। नए-नए फ़िक़ही ज्ञान-विज्ञान अस्तित्व में आए। नए-नए विभाग सामने आए जिनमें से कई विभागों की मैं निशानदेही कर चुका हूँ। इन नए विभागों पर अलग-अलग किताबें लिखी गईं। फिर इन किताबों के भी सारांश और ‘मुतून’ तैयार हुए। फिर इन ‘मुतून’ की भी व्याख्याएँ तैयार हुईं। यह गोया आंशिक रूप से फ़िक़्हे-इस्लामी के विभिन्न अध्यायों की आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान था। एक तो अस्ल फ़िक़्ह के ‘मुतून’ थे और अस्ल फ़िक़्ह की व्याख्याएँ थीं। फिर आंशिक व्याख्याओं की ‘मुतून’ और व्याख्याएँ तैयार हुईं। फिर जब ये व्याख्याएँ आ गईं और नए-नए विभाग भी आ गए तो फिर इस बात की कोशिश शुरू हुई कि ऐसी बड़ी-बड़ी किताबें तैयार की जाएँ जिनमें सारे फ़िक़ही भंडारों को तर्क के साथ एक व्यापक किताब में समो दिया गया होता कि अगर कोई फ़िक़्हे-इस्लामी का विस्तृत दृष्टिकोण जानना चाहे तो उन किताबों के ज़रिए से जानकारी प्राप्त करे। यह ‘मतूलात’ का दौर कहलाता है।
इन सब ज़मानों में बहुत सही तरीक़े से कोई विभाजन करना बड़ा मुश्किल है। ये बड़े overlaping दौर हैं। यह कहना कि अमुक सन् तक का दौर ‘मुतून’ का दौर था और अमुक सन् के बाद यह दौर समाप्त हो गया, शरहों (व्याख्याओं) का दौर शुरू हुआ। यह कहना दुरुस्त नहीं होगा। एक ज़माना ऐसा रहा जिसमें ‘मुतून’ भी लिखे जाते रहे और शरहें (व्याख्याएँ) भी लिखी जाती रहीं। शरहों के साथ-साथ शरहों के फ़ुटनोट भी लिखे जाते रहे। ‘मतूलात’ भी लिखी जाती रहीं। लेकिन समझने की ख़ातिर किसी-न-किसी तरह से उन ज़मानों को विभाजित किया जा सकता है। ये वे बड़ी-बड़ी किताबें हैं जिनका आज की चर्चा में परिचय अभीष्ट है। गोया पहले उसूल, जो धर्मों की मौलिक किताबें हैं, फिर ‘मुतून’, फिर ‘मुतून’ की शरहें, फिर शरहों की शरहें, फिर फ़ुटनोट, फिर फ़ुटनोट के स्पष्टीकरण और फिर विभिन्न विद्वानों के कमेंट्स। फिर विभिन्न मुफ़्ती लोगों के फ़तवे, जिनकी संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती चला जा रही है।
फ़िक़्ह और बौद्धिकता
चौथी-पाँचवीं सदी हिजरी में मुसलमानों के दरमियान बौद्धिकता का रिवाज बहुत बढ़ गया। यूनानी तार्किकता और दर्शन प्रचलित हो गया। बौद्धिकता को दिन-प्रतिदिन उरूज मिलने लगा। बौद्धिकता के बढ़ावे की वजह से मुसलमानों के तमाम ज्ञान विभाग बौद्धिकता से प्रभावित हुए। फ़िक़्ह भी प्रभावित हुई, उसूले-फ़िक़्ह की कला भी यूनान की बौद्धिक शैली से प्रभावित हुई और बजाय इसके कि अस्ल शरई आदेश पर चिन्तन-मनन किया जाता, या शरीअत के मूल उद्देश्य सर्वप्रथम ध्यान के केन्द्र होते, कुछ जगहों पर ऐसा महसूस होता है कि प्राथमिकता शरीअत के उद्देश्यों के बजाय शाब्दिक बहसें करने और तार्किक बारीकियाँ निकालने को प्राप्त हो गई। जो शरीअत के उद्देश्य थे वे पृष्ठभूमि में चले गए और शाब्दिक बहसें और दार्शनिक आपत्तियाँ तथा दार्शनिक उत्तर ज़्यादा नुमायाँ हो गए। यों कुछ लिखनेवाले मूल विषय से दूर होते चले गए। अल्लाह की किताब और अल्लाह की रसूल की सुन्नत (तरीक़ा) से सम्बन्ध, यों लगता है, उतना मज़बूत नहीं रहा जितना होना चाहिए था। बाद के धर्मशास्त्रियों के कथनों पर ज़ोर बढ़ता गया। यह चीज़ एक दृष्टि से लाभदायक भी थी, लेकिन कई दृष्टियों से हानिकारक भी थी।
हानिकारक तो इस दृष्टि से थी कि फ़िक़्हे-इस्लामी के अध्ययन के परिणामस्वरूप अल्लाह के प्रति जो निष्ठा और अल्लाह से सम्बन्ध पैदा होना चाहिए था वह इस तरह नहीं रहा। एक ज़ाहिर-परस्ती और शाब्दिकता और literalism का पहलू नुमायाँ हो गया। यह बहुत बड़ा नैतिक नुक़्सान था। दूसरा बड़ा ज्ञानपरक नुक़्सान यह था कि जब मुताख़्ख़िरीन यानी बादवाले फ़ुक़हा के कथन, इबारतें और बयानात ध्यान का अस्ल केन्द्र बन गए तो इज्तिहाद का पहलू इस दृष्टि से कमज़ोर होता चला गया। इज्तिहाद तो सीधा क़ुरआन और सुन्नत के आधार पर होगा। अगर क़ुरआन और सुन्नत पर ज़ोर रहेगा तो इज्तिहाद की प्रक्रिया जारी रहेगी। क़ुरआन और सुन्नत पर ज़ोर कम होगा तो इज्तिहाद की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे परिस्थितियों में इज्तिहाद की प्रक्रिया अगर शेष रहेगी भी तो बहुत-सीमित सतह पर रहेगी। वजह साफ़ ज़ाहिर है। जो सारगर्भिता या व्यापकता अल्लाह की किताब के शब्द में है वह किसी इंसान के शब्द में नहीं हो सकती। जो सारगर्भिता और सार्वभौमिकता अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शुभ कथनों में है, वह किसी फ़क़ीह (इस्लामी धर्मशास्त्री) के शब्दों में नहीं हो सकती। इसलिए पहली और दूसरी तीसरी सदी के मुज्तहिदीन के इज्तिहादात में जो व्यापकता मालूम होती है वह बाद के मुफ़्ती लोगों और फ़ुक़हा के कथनों में मालूम नहीं होती। इसकी वजह यह है कि बादवालों का सम्बन्ध और ताल्लुक़ बादवालों के कथनों से ज़्यादा रहा और अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत से कम रहा। लेकिन शिक्षा और शोध के इस तरीक़े का एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ। वह फ़ायदा यह था कि फ़ुक़हा ने जो इज्तिहादात किए थे और पहली और दूसरी सदी हिजरी में जो फ़िक़ही मसलक क़ायम हुए थे उनके एक-एक पहलू और एक-एक शब्द पर इतना अधिक ग़ौर किया गया, इतनी बारीकी से एक-एक चीज़ का जायज़ा लिया गया कि किसी चीज़ में किसी ग़लत-फ़हमी की सम्भावना नहीं रही। किसी एक राय को जब कई सौ वर्ष तक चिन्तन-मनन का विषय बनाया जाएगा तो इसमें किसी ग़लती और उलझन की सम्भावना बहुत कम रह जाएगी और हर चीज़ बहुत स्पष्ट होकर सामने आ जाएगी। यह उसका फ़ायदा भी हुआ। अब मैं एक-एक करके एक महत्वपूर्ण फ़िक़ही मसलक की महत्वपूर्ण किताबों का आरम्भिक और सरसरी परिचय आपके सामने कराता हूँ।
फ़िक़्हे-हनफ़ी की महत्वपूर्ण किताबें
सबसे पहले फ़िक़्हे-हनफ़ी को लेते हैं। चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से फ़िक़्हे-हनफ़ी सबसे पहले है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) शेष तीनों फ़ुक़हा से ज़माने की दृष्टि से मुतक़द्दिम (सबसे पहले) हैं इसलिए फ़िक़्हे-हनफ़ी क्रम में सबसे पहले आनी चाहिए। फ़िक़्हे-हनफ़ी के जो उसूल हैं, यानी वे मौलिक किताबें जिनपर फ़िक़्हे-हनफ़ी का आधार है, ये वे किताबें हैं जो इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के शागिर्द (शिष्य) इमाम मुहम्मद (रह॰) और इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) ने लिखी हैं। जिस व्यक्तित्व ने सबसे ज़्यादा इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) और उनके साथियों के इज्तिहादात को संकलित किया, वे इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी हैं, जो फ़िक़्हे-हनफ़ी के वास्तविक संकलनकर्ता हैं। इमाम मुहम्मद (रह॰) ने बहुत-सी किताबें लिखीं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी किताबों की संख्या 99 है, कुछ का कहना है कि एक हज़ार है। बहरहाल उनकी किताबें बड़ी संख्या में हैं और उनकी दो क़िस्में हैं। एक प्रकार की किताबें ‘ज़ाहिरुर-रिवायत’ कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की किताबों को ‘नादिरुर-रिवायत’ कहते हैं। इमाम मुहम्मद (रह॰) की छः किताबें वे हैं जो अत्यन्त प्रसिद्ध एवं प्रचलित हैं और पूरी फ़िक़्हे-हनफ़ी का आधार इन छः किताबों पर है। वे छः किताबें यह हैं—
(1) जामेअ सग़ीर (2) जामेअ कबीर (3) मबसूत या किताबुल-अस्ल (4) ज़ियादात (5) सियरे-कबीर (6) सियरे-सग़ीर।
ये छः किताबें फ़िक़्हे-हनफ़ी का आधार हैं और यही छः किताबें ‘कुतुबे-ज़ाहिरुर-रिवायत’ कहलाती हैं। उनके अलावा इमाम मुहम्मद की जितनी किताबें हैं वे सब ‘कुतुबे-नादिरुर-रिवायत’ कहलाती हैं। फ़िक़्हे-हनफ़ी में जो इज्तिहादात या कथन बयान हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तनद वे कथन एवं इज्तिहादात हैं जो इमाम मुहम्मद (रह॰) की पहली छः किताबों में बयान हुए हैं। ये पहली छः किताबें वे हैं जिनमें इमाम मुहम्मद (रह॰) ने इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के इज्तिहादात को प्रत्यक्ष रूप से बयान किया है।
इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) से जो चीज़ें इमाम मुहम्मद (रह॰) तक पहुँचीं वे भी इन किताबों में लिखी हुई हैं और यों ये किताबें फ़िक़्हे-हनफ़ी का आधार हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब किताबुल-मबसूत है जो किताबुल-अस्ल, भी कहलाती है। यह किताब अत्यन्त मोटी है और अनेक भागों में है। इस किताब से पता चलता है कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) किस तरह की तार्किकता से काम लेते थे। और किस तरह विभिन्न मामलों पर चिन्तन-मनन करके परिणाम तक पहुँचते थे। मैंने पहले एक चर्चा में बताया था कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की शोध एवं इज्तिहाद की शैली सामूहिक थी, व्यक्तिगत नहीं थी। इमाम साहब किसी एक मसले को अपने शिष्यों के सामने रखते थे। शिष्य उसपर बहस करते थे। इमाम साहब अपनी राय बयान करते थे। शिष्य उसपर आपत्ति करते थे और इमाम साहब उनका जवाब दिया करते थे और अन्ततः जब किसी एक राय पर सबका मतैक्य हो जाता था तो वह सर्वसम्मत राय लिख ली जाती थी। और अगर किसी एक राय पर सर्वसम्मति नहीं होता थी तो वह इख़्तिलाफ़ी राय भी लिख ली जाती थी। यह अक्सर बहसें ‘किताबुल-अस्ल’ या ‘किताबुल-मबसूत’ में इमाम मुहम्मद (रह॰) ने बयान की हैं। ज़ाहिर है कि इमाम मुहम्मद स्वयं भी असाधारण रूप से आलिम और विद्वान इंसान थे। वे स्वयं भी पहली पंक्ति के फ़ुक़हा में से थे और इमाम शाफ़िई (रह॰) जैसे बड़े फ़ुक़हा उनके शिष्यों में शामिल हैं। इमाम मुहम्मद ने स्वयं इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के साथ-साथ इमाम मालिक (रह॰) जैसे मुहद्दिस से भी ज्ञान प्राप्त किया। उनकी लिखी हुई यह किताब उक्त छः किताबों में नुमायाँ हैसियत रखती है।
इमाम मुहम्मद (रह॰) ने जब यह किताब लिखी तो यह बहुत लोकप्रिय हुई। लोगों ने इससे बहुत लाभ उठाया। बहुत जगहों पर उसके नुस्ख़े लोकप्रिय हुए। उस ज़माने में एक यहूदी था जो अरबी भी जानता था और मुसलमानों में रहने की वजह से फ़िक़्ह और शरीअत के मामलात की भी कुछ-न-कुछ जानकारी रखता था। इस यहूदी को कहीं से यह किताब हाथ लगी। उसने यह किताब पढ़ी तो कहा कि “यह तो तुम्हारे छोटे मुहम्मद का हाल है तो बड़े मुहम्मद का क्या हाल होगा।” यह कहकर उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। यह इस दर्जे की किताब है।
इमाम मुहम्मद की शेष किताबें जिनकी संख्या दर्जनों में है और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के दूसरे शिष्यों की किताबें, ये सब ‘नादिरुर-रिवायत’ कहलाती हैं और इनका दर्जा ‘कुतुबे-ज़ाहिरुर-रिवायत’ के बाद आता है, अगर दोनों में टकराव हो। दोनों किताबों में दो विभिन्न राय बयान की गई हों तो उस राय या उस पक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी जो ‘कुतुबे-ज़ाहिरुर-रिवायत’ में बयान किया गया है। ये सब किताबें छपी हुई मौजूद हैं। ‘जामेअ-सग़ीर’ और ‘जामेअ-कबीर’ दोनों मौजूद हैं, दोनों किताबें अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। दोनों किताबों की शरहें दर्जनों की संख्या में लिखी गईं। उनमें से कुछ व्याख्याएँ आज भी मौजूद हैं। कुछ व्याख्याएँ भारत में लिखी गईं जो प्रकाशित रूप में मौजूद हैं, और दर्जनों व्याख्याएँ वे हैं जो अभी मख़तूतात (हस्तलेखों) के रूप में मिस्र, इस्तंबोल, सीरिया और दुनिया के अनेक पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा मिस्र, दमिशक़ और इस्तंबोल के पुस्तकालयों में मौजूद हैं जहाँ अरबी भाषा के प्राचीन मख़्तूतात की संख्या लाखों में है।
इमाम मुहम्मद की ये छः किताबें चूँकि फ़िक़्हे-हनफ़ी का आधार हैं और उनमें तार्किकता का आधार बड़ा मज़बूत है, इसलिए जिन-जिन इलाक़ों में फ़िक़्हे-हनफ़ी प्रचलित होती गईं वहाँ ये किताबें भी प्रचलित होती गईं। इसलिए छात्रों और विद्वानों की सुविधा की ख़ातिर एक प्रसिद्ध हनफ़ी फ़कीह इमाम हाकिम शहीद मरूज़ी ने, जो एक जंग में शहीद हो गए थे और इस वजह से हाकिम शहीद कहलाते हैं, इन छः किताबों का सारांश तैयार किया, और इसका नाम रखा ‘अल-काफ़ी फ़ी फ़ुरूइल-हनफ़िया’। यह किताब तीन भागों में है। अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन एक ज़माने में अत्यन्त लोकप्रिय किताब रही। यह इमाम मुहम्मद की छः किताबों का सारांश है।
इस सारांश की व्याख्या एक बड़े प्रसिद्ध हनफ़ी फ़क़ीह शम्सुल-अइम्मा अस-सरख़सी ने की। वे अपने ज़माने के इतने बड़े इमाम थे कि लोगों ने उनका नाम शम्सुल-अइम्मा रखा, यानी तमाम इमामों के सूरज। हनफ़ी फ़ुक़हा में छः फ़ुक़हा शम्सुल-अइम्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे बड़े शम्सुल-अइम्मा सरख़सी हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि बारह वर्ष तक एक कुएँ में क़ैद रहे और कुएँ में बैठकर उन्होंने कई किताबें लिखीं, जिनमें एक यह किताब अल-काफ़ी की व्याख्या है जो तीस भागों में है। उनमें लगभग बारह भाग उन्होंने जेल में बैठकर डिक्टेट कराए। उनके शिष्य कुएँ की मुंडेर पर आकर बैठ जाते थे। शिक्षक महोदय अन्दर से बोलते जाते थे और शिष्य लिखते जाते थे। बारह भाग इस तरह लिखवाए गए और शेष भाग रिहाई के बाद पूरे किए। इमाम मुहम्मद की ‘अस-सियर अल-कबीर’ जो अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून पर बहुत व्यापक किताब थी, उसकी एक व्यापक व्याख्या भी उन्होंने इसी बावली या कुएँ में से डिक्टेट कराई और उसकी व्याख्या लिखवाई। शिष्यों ने लिखी। आज पाँच भागों में हमारे पास मौजूद है। ये व्याख्याएँ पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बेरूत, भारत और मिस्र में कई बार छप चुकी हैं और हर जगह उपलब्ध हैं। गोया ‘किताबुल-मबसूत’ जो आज हर बड़े इस्लामी पुस्तकालय में मौजूद है यह सीधे इमाम मुहम्मद के विचारों और इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के इज्तिहादात की व्याख्या है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के इज्तिहादात इमाम मुहम्मद (रह॰) की किताबों के ज़रिए सुरक्षित हुए। इमाम मुहम्मद की छः किताबें ‘अल-काफ़ी’ के रूप में संक्षिप्त रूप में तैयार हुईं और इस संक्षिप्त रूप की व्याख्या इमाम सरख़सी ने लिखी।
फ़िक़्हे-हनफ़ी के मुतून
जब ‘मुतून’ का दौर आया तो फ़िक़्हे-हनफ़ी के बहुत सारे ‘मुतून’ तैयार किए जाने लगे। जैसे-जैसे इस्लामी साम्राज्य फैल रहा था फ़िक़्हे-हनफ़ी भी फैल रही थी। फ़िक़्हे-मालिकी मुस्लिम जगत् के पश्चिम में और फ़िक़्हे-शाफ़िई मध्य-पूर्व में फैल रही थी। और फ़िक़्हे-हंबली अरब द्वीप के पूरब और उत्तर में फैल रही थी। जैसे-जैसे फ़िक़्ह फैलती गई नए-नए इज्तिहादात होते गए। अब आवश्यकता महसूस हुई कि इस सारे भंडार को इस तरह से एक ‘मत्न’ के रूप में तैयार किया जाए कि यह ‘मत्न’ लोगों के लिए याद करना आसान हो जाए।
यह तो मालूम नहीं कि सबसे पहले फ़िक़्हे-हनफ़ी का ‘मत्न’ किसने लिखा, लेकिन जो ‘मत्न’ सबसे पहले लोकप्रिय हुआ और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ वह अल्लामा क़ुदूरी का लिखा हुआ ‘मत्न’ था जिसको ‘मुख़्तसर अल-क़ुदूरी’ कहा जाता है। ‘क़ुदूरी’ ढाई तीन सौ पृष्ठों की एक संक्षिप्त-सी किताब है, लेकिन इसमें फ़िक़्हे-हनफ़ी की तमाम समस्याओं को सरलतम भाषा में सारगर्भिता के साथ बयान कर दिया गया है। उस समय तक फ़िक़्हे-हनफ़ी में जितने इज्तिहादात हुए थे और जितनी समस्याओं का जवाब दिया गया था उनमें मौलिक और अहम समस्याओं का चयन करके अल्लामा क़ुदूरी ने इस किताब में जमा कर दिया।
यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई और जब से लिखी गई है उस समय से लेकर आज तक दुनिया-भर में एक पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान, भारत, बाँग्लादेश, बर्मा, अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशिया, मिस्र और कई अन्य देशों में जहाँ-जहाँ फ़िक़्हे-हनफ़ी की शिक्षा दी जा रही है वहाँ यह किताब पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाई जाती है। किसी ज़माने में इसको कंठस्थ करने का प्रचलन भी था। जब इस किताब को बच्चे कंठस्थ कर लिया करते थे तो पूरे जीवन फ़िक़्हे-हनफ़ी की जड़ उनके हाथ में रहती थी। अब ज़बानी याद करने का रिवाज तो समाप्त हो गया, लेकिन पढ़ने का रिवाज अभी तक मौजूद है। क़ुदूरी की बहुत-सी व्याख्याएँ लिखी गईं। उर्दू में भी लिखी गईं। फ़ारसी, अरबी और अन्य भाषाओं में भी लिखी गईं।
हिदाया
क़ुदूरी के लिखे जाने के कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध फ़क़ीह अल्लामा बुरहानुद्दीन मर्ग़िनानी थे। यह वर्तमान उज़्बेकिस्तान के इलाक़े फ़र्ग़ाना के क़रीब मर्ग़िनान नाम के एक इलाक़े के रहनेवाले थे। उन्होंने यह महसूस किया कि अल्लामा क़ुदूरी की संक्षिप्त और इमाम मुहम्मद (रह॰) की ‘जामेअ-सग़ीर’ में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो एक-दूसरे के यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्होंने समझा कि ये दोनों प्रकार की समस्याएँ किसी एक किताब में इकट्ठा कर देनी चाहिएँ। उन्होंने क़ुदूरी और ‘जामेअ-सग़ीरा’ का तुलनात्मक जायज़ा लिया तो पता चला कि दोनों में कुछ जगह दोहराव है और कुछ जगह अलग समस्याएँ हैं जो किसी एक या दूसरी किताब में नहीं मिलतीं। उन्होंने दोहराव को निकाल दिया और जो समस्याएँ किसी एक किताब में थीं और दूसरी में नहीं थीं उनको एक जगह जमा किया और एक नया टेक्स्ट तैयार करके उसका नाम ‘बिदायतुल-मुब्तदी’ रखा।
‘बिदायतुल-मुब्तदी’ एक तरह से ‘जामेअ-सग़ीर’ और क़ुदूरी का एक combination था। अल्लामा मर्ग़िनानी ने बदाए ‘अल-मुबतदी’ तैयार करके एक बड़ी सेवा अंजाम दी। फिर उन्होंने स्वयं ही ‘बिदायतुल-मुब्तदी’ की एक व्याख्या भी लिखी। कहा जाता है कि वह बहुत मोटी किताब थी। इसके बारे में बहुत अधिक विवरण मिलते हैं। किसी का कहना है कि चालीस भागों में और किसी का कहना कि पचास भागों में थी। किसी का कहना है कि सत्तर भागों में थी। अल्लामा मर्ग़िनानी ने इस व्याख्या का नाम ‘किफ़ायतुल-मुन्तही’ रखा था। ‘किफ़ायतुल-मुन्तही’ यानी जो फ़िक़्हे-इस्लामी का फ़ाइनल विद्यार्थी हो उसको यह किताब काफ़ी होगी। यह उसके शाब्दिक अर्थ हैं। जब उन्होंने यह किताब तैयार कर ली, तो उन्होंने सोचा कि इतनी विस्तृत किताब को कौन पढ़ेगा। इसलिए इस किताब का ऐसा सारांश तैयार करना चाहिए जो संक्षिप्त हो और आम लोग उसको पढ़कर लाभान्वित हो सकें। यह सोचकर उन्होंने ‘किफ़ायतुल-मुन्तही’ का सारांश तैयार किया जो ‘हिदाया’ के नाम से हर जगह प्रसिद्ध है। इसके सैंकड़ों एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं और इसका उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो और फ़ारसी अनुवाद भी उपलब्ध है। यह उस समय से लेकर आज तक हर जगह पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ी जाती है। पाकिस्तान, भारत, बाँग्लादेश, मध्य एशिया, मिस्र, अफ़ग़ानिस्तान, सीरिया, जॉर्डन और जहाँ-जहाँ फ़िक़्हे-हनफ़ी पढ़ी और पढ़ाई जाती है वहाँ ‘हिदाया’ भी पढ़ाई जाती है।
‘हिदाया’ फ़िक़्हे-हनफ़ी की अत्यन्त मुस्तनद किताबों में से एक है। इसकी तार्किक शैली बड़ी बौद्धिक, इसका अंदाज़ अत्यन्त ज्ञानपरक, इसकी शैली अत्यन्त साइंटिफ़िक और संक्षिप्त और precise (सटीक) किताब है। इसमें एक शब्द भी अधिक नहीं है। ‘हिदाया’ के महान लेखक अपनी बात को इतने सलीक़े से कहते हैं कि पढ़नेवाला एक बार उनकी शैली से परिचित हो जाए तो वह बड़ी आसानी से किताब से लाभान्वित हो सकता है। उदाहरण के रूप में जब उन्हें यह कहना हो कि इस मामले में इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की राय यह है और इमाम मुहम्मद (रह॰) और इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) की राय यह है तो वह उनके नाम नहीं लेते, क्योंकि इन सब फ़िक़्ह के इमामों के पूरे नाम लिखने में तो ख़ासी जगह लग जाती है। उदाहरणार्थ ‘व इन-द अबी हनीफ़ा’ में ‘इन-द’ अलग शब्द है, ‘अबी’ अलग और ‘हनीफ़ा’ अलग। इसकी बजाय वह लिखते हैं ‘व-लहू’, ‘व-लहुमा’। यह उनका एक अंदाज़ है कि ‘लहू’ से पता चलता है कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) का दृष्टिकोण यह है और ‘हुमा’ से पता चलता है कि शेष दो साथियों का दृष्टिकोण यह है। और अगर वे कहें कि ‘व-इन-दना’ तो मतलब है हमारे तीनों इमामों का दृष्टिकोण यह है। इस तरह से उन्होंने कुछ प्रतीक बनाए हैं जिनके ज़रिये उन्होंने कुछ और संक्षेप से काम लिया है। यह किताब फ़िक़्हे-हनफ़ी की कुछ मुस्तनद तरीन किताबों में से है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से इस किताब को समझकर पढ़ ले और इसके तर्क और इस्तिदलाल से गहराई के साथ परिचित हो जाए तो न केवल बहुत अच्छा फ़क़ीह बन जाता है, न केवल फ़ुक़हा की तर्क शैली और इज्तिहाद की शैली पर उसको पकड़ प्राप्त हो जाती है बल्कि फ़िक़्हे-हनफ़ी की कुंजी उसके हाथ लग जाती है।
इस किताब की लोकप्रियता के सामने आवश्यकता महसूस की गई कि इसका एक व्यापक संक्षिप्त रूप तैयार किया जाए। यह संक्षिप्त रूप एक फ़क़ीह ताजुश-शरीआ मुहम्मद-बिन-सदरुश-शरीआ ने तैयार किया जो अल्लामा मर्ग़िनानी के लगभग सौ डेढ़ सौ वर्ष बाद आए। इस संक्षिप्त रूप का नाम उन्होंने ‘वक़ाया’ रखा। ‘वक़ाया’ एक ‘मत्न’ क़रार पाया और क़ुदूरी के बाद फ़िक़्हे-हनफ़ी का दूसर लोकप्रियतम ‘मत्न’ क़रार दिया जाता है। यह वास्तव में ‘हिदाया’ का संक्षिप्त रूप है। यानी इसमें क़ुदूरी और ‘जामेअ सग़ीर’ की मौलिक समस्याएँ भी आ गईं और कुछ वे समस्याएँ जिनकी वृद्धि अल्लामा मर्ग़िनानी ने की थी वे भी आ गईं। विस्तृत विवरण को निकालते हुए जो महत्वपूर्ण और मौलिक समस्याएँ और नियम थे वे सब उन्होंने इस नए ‘मत्न’ में समो दिए। यह ‘मत्न’ भी उस समय से पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाया जाता है। जब यह ‘मत्न’ लोकप्रिय हो गया तो उसी लेखक के नवासे सदरुश-शरीआ उबैदुल्लाह-बिन-मसऊद ने इसकी व्याख्या लिखी जो ‘शरहे-वक़ाया’ के नाम से प्रसिद्ध है। ‘शरहे-वक़ाया’ भी आज तक एक पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाई जाती है। अगरचे ‘शरहे-वक़ाया’ का वह दर्जा नहीं है जो ‘हिदाया’ का है, लेकिन यह भी एक लोकप्रिय किताब है और आज तक पढ़ाई जा रही है। ‘शरहे-वक़ाया’ की भी बहुत-सी शुरूह (व्याख्याएँ), बहुत-से फ़ुट नोट्स लिखे गए जिनमें उर्दू, फ़ारसी और अरबी में लिखे जानेवाले नोट्स और हाशिये भी शामिल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भी लिखे गए और बाहर भी लिखे गए।
कंज़ुद्दक़ाइक़
‘क़ुदूरी’ और ‘वक़ाया’ के बाद तीसरा लोकप्रियतम ‘मत्न’ और फ़िक़्हे-इस्लामी के भंडार का शायद सबसे निराला मत्न ‘कंज़ुद्दक़ाइक़’ कहलाता है। इसको एक प्रसिद्ध फ़क़ीह, क़ुरआन के टीकाकार और मुतकल्लिम अल्लामा हाफ़िज़ुद्दीन निसफ़ी ने सातवीं सदी हिजरी के अन्त में लिखा था। उनकी एक तफ़सीर (टीका) भी ‘मदारिकुत्तंज़ील’ के नाम से है। उसूले-फ़िक़्ह पर भी उन्होंने काम किया है। कंज़ुद्दक़ाइक़ के नाम से उन्होंने जो ‘मत्न’ तैयार किया है वह तमाम ‘मुतून’ से ज़्यादा संक्षिप्त और व्यापक है। इतना संक्षिप्त और व्यापक कि इस्लामी साहित्य में न उस संक्षिप्तीकरण का उदाहरण मिलता है और न उस सारगर्भिता का। कुछ स्थानों पर अपने संक्षिप्तीकरण की वजह से यह एक पहेली मालूम होती है। इसके उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं और एक उदाहरण हम लोग बहुत अधिक दिया करते हैं। इससे अनुमान होता है कि किस तरह से वह एक लम्बी बहस को समेटकर अति संक्षिप्त इबारत में बयान करते हैं।
समस्या यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज़ हिबा कर दे या हदिया (भेंट) दे दे और बाद में इस हदिये या हिबा को वापस लेना चाहे तो किन परिस्थितियों में हदिया वापस लिया जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं लिया जा सकता। यह एक बहुत मतभेदपूर्ण समस्या है और इसपर बहुत बहसें हुई हैं। नैतिक दृष्टि से तो हदिया वापस लेना बुरी बात है और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसको हतोत्साहित किया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर क़ानूनी दृष्टि से कोई अपना दिया हुआ हदिया वापस लेना चाहे तो इसके लिए क़ानूनी गुंजाइश है कि नहीं। अदालत में अगर कोई व्यक्ति यह दावा लेकर आए कि मैं अपना हदिया वापस लेना चाहता हूँ तो अदालत क्या कहेगी। अदालत तो नैतिक दृष्टि या शिष्टाचार और ‘मुस्तहबात’ पर नहीं जाती, वह तो ख़ालिस क़ानून की रौशनी में फ़ैसला करती है।
इस मामले में हनफ़ी फ़ुक़हा का दृष्टिकोण यह है कि सात स्थितियाँ ऐसी हैं कि जिनमें हदिया वापस नहीं लिया जा सकता। शेष हर स्थिति में लिया जा सकता है। अगर वे सात स्थितियाँ आपको कहीं बयान करनी हों तो कम-से-कम एक पूरा पृष्ठ तो लिखना पड़ेगा। अल्लामा निसफ़ी ने इस पूरी बहस को एक वाक्य में बयान किया है। वे कहते हैं والرجوع فی الہبۃ دمع خرقہ यानी “हिबा में रुजू करने का मामला ‘दमा ख़िरक़ा’ है। यहाँ ‘द’ से मुराद है ज़्यादती यानी इज़ाफ़ा। अगर कोई चीज़ जो आपने हिबा में किसी को दे दी थी और बाद में उसमें कोई इज़ाफ़ा हो गया। उदाहरणार्थ आपने बकरी का बच्चा दिया था, उसने पाल-पोसकर पूरी बकरी कर दी। तो अब आपके लिए उसका वापस लेना जायज़ नहीं। अगर हिबा की हुई चीज़ ज़्यादा हो जाए और उसमें इज़ाफ़ा हो जाए तो उसको वापस लेना जायज़ नहीं है। ‘म’ से मुराद है मौत। हिबा करनेवाला, या वह चीज़ जो हिबा की गई थी, उसकी मौत हो गई। उदाहरणार्थ भैंस हदिये में दी थी और वह मर गई तो इन सब स्थितियों में आप हिबा वापस नहीं ले सकते। ‘ऐन’ का मतलब है एवज़ यानी आपने कोई चीज़ दी और उसने भी बदले में कोई चीज़ दे दी। जैसा कि शादी-ब्याह में आप जोड़ा देते हैं और एवज़ में आपको भी जोड़ा दे दिया जाता है। देनेवाले को भी पता होता है कि बदले में कुछ मिलेगा और लेनेवाले को भी पता होता है कि बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगरचे यह हिबा कहलाता है, लेकिन अमलन इसकी हैसियत हिबा से भिन्न होती है। तो अगर किसी हिबा का एवज़ दे दिया जाए तो वह हिबा वापस लेना भी जायज़ नहीं है। इस तरह से मात्र एक-एक अक्षर के ज़रिये से उन्होंने यह बताया कि वे कौन-सी जगहें हैं जहाँ हिबा वापस नहीं लिया जा सकता।
एक और जगह विचाराधीन मसला यह है कि एक व्यक्ति जिसपर ग़ुस्ल वाजिब था, वह कुएँ में गिर गया। उदाहरणार्थ वह डोल निकालने गया था या पानी लेने गया था और कुएँ के अन्दर गिर गया। जब गिर गया तो लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकला तो पूरा शरीर भीग चुका था, क्योंकि पानी में डुबकी लगा चुका था। अब क्या आदेश है? इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) कहते हैं कि वह व्यक्ति पहले की तरह नापाक और हालते-जनाबत में है। मात्र कुएँ में गिरकर भीग जाने से उसका ग़ुस्ल नहीं हुआ। वह व्यक्ति अब भी नापाक है और उसके गिर जाने की वजह से पानी भी नापाक हो गया। इमाम अबू-यूसुफ़ कहते हैं कि इस व्यक्ति का ग़ुस्ल तो नहीं हुआ, लेकिन पानी पाक ही समझा जाएगा। इमाम मुहम्मद कहते हैं कि इस व्यक्ति का ग़ुस्ल हो गया और पानी भी पाक है। तीनों के विस्तृत तर्क हैं। आप उसको लिखेंगे तो चार पाँच पृष्ठ भर जाएँगे। इमाम निसफ़ी ने इस सारी बहस को एक वाक्य में यों लिखा है कि ’ومسئلۃ البشر جحط‘ चूँकि हनफ़ी फ़ुक़हा में सबसे पहला दर्जा इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) का है। इसलिए सबसे पहले उनकी राय बयान की है। ‘जीम’ से मुराद है नजिस। दोनों नजिस यानी नापाक हैं यानी पानी भी नजिस हो गया और वह व्यक्ति पहले की तरह नजिस रहा। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के बाद दूसरा दर्जा इमाम अबू-यूसुफ़ का है इसलिए अब उनका मसलक बयान किया है। ‘ह’ से मुराद ‘अला हालिहा’ यानी दोनों अपने हाल पर हैं। दोनों अपने हाल पर ही रहेंगे, कुआँ भी पाक रहेगा और यह व्यक्ति भी नापाक रहेगा। तीसरी राय इमाम मुहम्मद की है जिनका दर्जा इन दोनों लोगों के बाद है। ‘त’ से मुराद ताहिर, यानी कुआँ भी पाक है और आदमी भी पाक हो गया।
अब उन्होंने ‘ज-ह-त’ से पूरा मसला बयान कर दिया। कंज़ुद्दक़ाइक़ इस तरह की किताब है। कंज़ुद्दक़ाइक़, क़ुदूरी और वक़ाया, इन तीनों को ‘मुतूने-सलासा’ कहा जाता है। जब कहा जाए कि ‘मुतूने-सलासा’ में यह बात बयान हुई है तो इससे मुराद ये तीन ‘मुतून’ होंगे। जिस तरह से शेष ‘मुतून’ की शरहें लिखी गईं इस तरह कंज़ुद्दक़ाइक़ की भी शरहें लिखी गईं।
कंज़ुद्दक़ाइक़ की दो शरहें बड़ी प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक व्याख्या ‘तबईनुल-हक़ाइक़’ है। यह एक प्रसिद्ध फ़क़ीह और मुहद्दिस अल्लामा ज़ीलई की किताब है। इसमें तार्किकता पर बहुत बल दिया गया है। कोई बात ‘कंज़ुद्दक़ाइक़’ में क्यों कही गई है और इसकी दलील क्या है, यह विवरण ‘तबईनुल-हक़ाइक़’ में मिलता है। यह किताब तीन मोटे भागों में है।
दूसरी व्याख्या जो ज़्यादा विस्तृत है और आठ भागों में है। इसका नाम ‘अल-बहरुर्राइक़’ है। इसको अल्लामा इब्ने-नज्म ने लिखा है। अल्लामा इब्ने-नज्म की इस व्याख्या में मालूमात की अधिकता तथा उदाहरणों और आंशिक आदेशों को समेट लिया गया है। ये दोनों व्याख्याएँ मिलकर एक-दूसरे की पूर्ति करती हैं। एक व्याख्या में तर्क ज़्यादा है। दूसरी व्याख्या में उदाहरण ज़्यादा हैं।
इन चार ‘मुतून’ के अलावा फ़िक़्हे-हनफ़ी में दो और ‘मुतून’ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक ‘मुख़्तार’ के नाम से है जो अल्लामा मूसिली का लिखा हुआ है। मूसिल जो इराक़ का शहर है। उसकी व्याख्या ‘अल-इख़्तियार शरह मुख़तार’ के नाम से उन्होंने स्वयं ही लिखी थी। यह किताब भी बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत-सी जगहों में पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ाई जाती है।
बदाइउस्सनाइअ
आख़िरी ‘मत्न’ ‘मजमउल-बहरैन’ के नाम से है। यह इतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना शेष ‘मुतून’ लोकप्रिय हैं। फ़िक़्हे-हनफ़ी की एक और किताब जो वास्तव में एक ‘मत्न’ की व्याख्या है और बहुत लोकप्रिय और बेहतरीन किताब है। इसका नाम ‘बदाइउस्सनाइअ फ़ी तर्तीबिश-लशराइअ’ है। एक ख़ास पहलू से यह किताब आप लोगों के लिए यह ख़ास दिलचस्पी की किताब है। पाँचवीं और छठी सदी हिजरी के एक बुज़ुर्ग अल्लामा अलाउद्दीन समरक़ंदी ने ‘तोहफ़तुल-फ़ुक़हा’ के नाम से एक किताब लिखी थी। यह एक ‘मत्न’ था जिसमें उन्होंने क़ुदूरी में कुछ ‘मसाइल’ की वृद्धि करके और क़ुदूरी के क्रम को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में पेश किया था। उन्होंने यह महसूस किया कि क़ुदूरी के ज़माने से लेकर अब तक कुछ नई समस्याएँ सामने आई हैं जो क़ुदूरी में नहीं हैं। इस तरह क़ुदूरी के क्रम में कुछ दृष्टि से पुनरीक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने इन समस्याओं की वृद्धि करके क़ुदूरी के क्रम को नए सिरे से संकलित किया और एक किताब तोहफ़तुल-फ़ुक़हा के नाम से लिख दी। जिन बुज़ुर्गों ने यह किताब लिखी थी उनके एक नौजवान शिष्य अल्लामा अलाउद्दीन कासानी थे। उन्होंने तीस-बत्तीस वर्ष की उम्र में इस किताब की व्याख्या लिखी। जब उन्होंने व्याख्या लिखकर अपने उस्ताद को दिखाई तो वे इतने ख़ुश हुए और उन्होंने इस किताब को इतना पसंद किया कि शिष्य को अपना बेटा और फिर अपना दामाद बना लिया। उनकी एक बेटी थीं जिनका नाम फ़ातिमा था, जो बड़ी फ़क़ीह थीं, स्वयं उन्होंने अपने बाप से फ़िक़्ह सीखी थी। उनके पिता ने उनकी शादी अपने इस शिष्य से कर दी। अब ये दोनों यानी अल्लामा अलाउद्दीन कासानी और उनकी पत्नी फ़ातिमा मिलकर फ़िक़ही मामलों पर चिन्तन-मनन करते थे, फ़िक़्ह पढ़ाया करते थे और लोगों के सवालात के जवाबात दिया करते थे।
जब तक बेटी के पिता अल्लामा अलाउद्दीन समरक़ंदी ज़िन्दा रहे, उनके दर्स (क़ुरआन पाठ) का हल्क़ा (ग्रुप) क़ायम रहा, जिसमें उनकी बेटी और दामाद भी हाथ बटाते रहे। यों इन तीनों की मौजूदगी से एक केन्द्र अस्तित्व में आ गया जहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए दूर-दूर से लोग आया करते थे। जब ससुर का देहान्त हो गया तो बेटी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि वे फ़िक़्ह की आलिमा बन गई थीं और लोगों के फ़िक़ही सवालात का जवाब दिया करतीं और वे और उनके पति यानी अल्लामा कासानी मिलकर फ़िक़्ह की यह अकैडमी चलाते थे। ये दोनों मिलकर फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाया करते थे। कुछ समय के बाद अल्लामा कासानी की इन पत्नी का देहान्त हो गया तो उनकी बेटी अपने पिता यानी ‘बदाइउस्सनाइअ’ के लेखक दोनों मिलकर फ़तवा देने लगे। बेटी फ़तवा दिया करती तो पिता उसकी पुष्टि एवं सत्यापन करते और पिता फ़तवा देते तो बेटी चेक करके पुष्टि एवं सत्यापन करती कि फ़तवा दुरुस्त है या नहीं। उन दोनों के दस्तख़त से फ़तवा जारी होता था। यह किताब ‘बदाइउस्सनाइअ’ फ़िक़्हे-हनफ़ी की बेहतरीन किताब है। इससे बेहतर कोई किताब फ़िक़्हे-हनफ़ी में नहीं लिखी गई, बल्कि अगर यह कहा जाए तो ग़लत नहीं होगा कि पूरे फ़िक़ही भंडार में कोई किताब अपने तार्किक क्रम की दृष्टि से इतने बेहतरीन अंदाज़ में नहीं लिखी गई। जब वह एक मसले (समस्या) को लेते हैं तो अत्यन्त बौद्धिक एवं तार्किक ढंग से उसको स्पष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ अगर वे यह बयान कर रहे हों कि शरीअत में शराब पीना हराम है और शराब की सज़ा शरीअत ने यह नियुक्त की है, तो इस किताब में मसला बयान करने का अंदाज़ ऐसा होगा कि पढ़नेवाला ख़ुद-ब-ख़ुद उनके विचारों एवं रायों से प्रभावित होता चला जाएगा। यानी उदाहरण के रूप में उन्होंने इस मसले को इस तरह से शुरू किया होगा कि मशरूबात (पेय पदार्थ) इंसान की मौलिक आवश्यकता हैं। ज़ाहिर है इस बात से कोई मतभेद नहीं कर सकता। मशरूबात की दो क़िस्में हैं। कुछ मशरूबात जायज़ हैं और कुछ नाजायज़ हैं। नाजायज़ मशरूबात की दो किस्में हैं। कुछ वे नाजायज़ मशरूबात जिनको शरीअत ने स्पष्ट रूप से नाजायज़ क़रार दिया है और कुछ वे हैं जिनको फ़ुक़हा ने इज्तिहाद के ज़रिये नाजायज़ क़रार दिया है। जिन मशरूबात को शरीअत ने हराम क़रार दिया है उनकी फिर और दो क़िस्में हैं। कुछ मशरूबात के पीने पर सज़ा नियुक्त है और कुछ के लिए नहीं। इस तरह से तार्किक दृष्टि से हर-हर वाक्य इस तरह है कि उससे कोई आदमी मतभेद नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको कोई बात सरसरी तौर पर बुद्धि के ख़िलाफ़ मालूम हो। और उसपर भी आप कुछ ग़ौर करें तो पता चलेगा कि अल्लामा कासानी की राय में बड़ा वज़न है, और इस मसले में दोनों दृष्टिकोण एक साथ पाए जा सकते हैं। वह बात भी दुरुस्त हो सकती है जो इस किताब में है और जो आप समझते हैं वह भी दुरुस्त है।
इस तरह से उन्होंने पूरे फ़िक़्ह के संग्रहों को संकलित कर दिया। यह किताब आठ भागों में है और कई बार छपी है। पाकिस्तान, भारत, अफ़ग़ानिस्तान, मिस्र, सीरिया, लेब्नान और बहुत-सी दूसरी जगहों में यह किताब छपी है। इसका उर्दू अनुवाद भी उपलब्ध है। अगरचे वह ऐसा अनुवाद है जिसको समझने के लिए अरबी जानना ज़रूरी है। जो आदमी अरबी और फ़िक़्ह जानता हो वह तो इस अनुवाद से लाभान्वित हो सकता है। जो आदमी अरबी भाषा और फ़िक़्ह से अपरिचित हो उसके लिए अनुवाद पढ़ना ऐसा ही मुश्किल है जिस तरह कि अस्ल किताब को पढ़ना। यह तो सम्भव है कि कोई ऐसा आदमी जिसकी अरबी तो कमज़ोर हो, लेकिन फ़िक़्ह अच्छी हो, वह लाभ उठा ले। या जिसकी फ़िक़्ह कमज़ोर हो, लेकिन अरबी अच्छी हो वह भी लाभ उठा ले। वरना जो आदमी बिलकुल अरबी और फ़िक़्ह नहीं जानता उसके लिए इस उर्दू अनुवाद से लाभान्वित होना बहुत मुश्किल होगा।
एक और मत्न ‘तनवीरुल-अबसार’ था जो आख़िरी है और सम्भवतः सातवीं या आठवीं सदी हिजरी में लिखा गया है। इसकी व्याख्या ‘अद-दुर्रुल-मुख़्तार’ के नाम से लिखी गई। ‘अद-दुर्रुल-मुख़्तार’ भी बड़ी प्रसिद्ध हुई। ‘अद-दुर्रुल-मुख़्तार’ की व्याख्या या फ़ुटनोट ‘रद्दुल-मुहतार’, के नाम से लिखे गए। ‘रद्दुल-मुहतार’ फ़िक़्हे-हनफ़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों में से है। और फ़िक़्हे-हनफ़ी में अक्सर एवं अधिकतर जब फ़तवा दिया जाता है तो ‘रद्दुल-मुहतार’ के हवाले से दिया जाता है। ‘रद्दुल-मुहतार’ बड़ी मोटी किताब है जो सात भागों में है और पिछली सदी से फ़तवे के एक अति महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर चली आ रही है। पिछली सदी में एक बुज़ुर्ग अल्लामा इब्ने-आबिदीन शामी, दमिशक़ के रहनेवाले थे। उन्होंने यह किताब लिखी थी। यह किताब बहुत जल्द न केवल दुनियाए हनफ़ियत, बल्कि इससे बाहर भी बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गई।
फ़िक़्हे-मालिकी की महत्वपूर्ण किताबें
फ़िक़्हे-हनफ़ी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण फ़िक़ही मसलक फ़िक़्हे-मालिकी है। फ़िक़्हे-मालिकी में भी कुछ उसूल हैं, कुछ ‘मुतून’ हैं, कुछ ‘मुतून’ की व्याख्याएँ हैं, फिर व्याख्याओं के फ़ुटनोट हैं, फिर विभिन्न उप शाखाओं पर अलग-अलग किताबें हैं, फिर इन किताबों की व्याख्याएँ हैं, फिर शेष किताबें हैं। किताबों के दर्जों एवं वर्गों का जो क्रम फ़िक़्हे-हनफ़ी के बारे में बयान किया गया है वही क्रम फ़िक़्हे-मालिकी में भी है।
फ़िक़्हे-मालिकी की दो मूल किताबें : मुवत्ता और मुदव्वना
फ़िक़्हे-मालिकी की अस्ल बुनियादें और उसूल दो हैं। एक से तो हम सब परिचित हैं यानी मुवत्ता इमाम मालिक, जो हदीस की किताब भी है और फ़िक़्ह की किताब भी है। इस्लामियात का हर विद्यार्थी मुवत्ता इमाम मालिक से वाक़िफ़ है। मुवत्ता इमाम मालिक के महत्व का अनुमान इससे करें कि शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी के शब्दों में चारों फ़ुक़हा के फ़िक़ही इज्तिहादात की जड़ और आधार मुवत्ता इमाम मालिक में मिलती है। शाह साहब ने कहा है कि मुवत्ता इमाम मालिक में जो-जो फ़िक़ही रायें और इज्तिहादात पर आधारित संग्रह मौजूद है वह सारे-का-सारा मौलिक रूप से हज़रत उमर-बिन-ख़िताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इज्तिहादात पर आधारित है। और इन्हीं दोनों प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्तिहादात के आधार पर चारों फ़िक़हें संकलित हुई हैं। और चूँकि उनके इज्तिहादात को इमाम मालिक (रह॰) ने अपनी इस किताब में समोया है। इसलिए चारों फ़िक़ही मसलकों की जड़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद हैं। शाह साहब की राय का समर्थन इस वास्तविकता से भी होता है कि मुवत्ता इमाम मालिक बिना मसलक का भेद किए हर फ़िक़्ह में लोकप्रिय है और तमाम बड़े-बड़े फ़िक़ही मसलकों के फ़ुक़हा मुवत्ता इमाम मालिक में उपलब्ध सामग्री और तर्क से प्रमाण लेते हैं। इन कारणों के आधार पर शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी यह समझते थे कि अगर मुवत्ता इमाम मालिक को दर्से-हदीस का आधार बनाया जाए तो फ़िक़ही मसलकों में जो मतभेद है उसको कम किया जा सकता है। निश्चय ही यह बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि अगर मुवत्ता इमाम मालिक को दर्से-हदीस का आधार बनाया जाए तो तमाम फ़िक़ही मसलकों को एक-दूसरे के क़रीब लाया जा सकता है। इसके अलावा इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) और इमाम मालिक (रह॰) को कई बार विचारों के आदान-प्रदान का मौक़ा मिला। दोनों ने एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझा। फिर इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के शागिर्दों में इमाम मुहम्मद (रह॰) जो फ़िक़्हे-हनफ़ी के अस्ल संकलनकर्ता हैं, वह इमाम मालिक (रह॰) के भी प्रत्यक्ष रूप से शिष्य हैं। इमाम मालिक (रह॰) के प्रभाव उनकी किताबों के द्वारा हनफ़ी फ़ुक़हा तक पहुँचे हैं। फिर इमाम शाफ़िई (रह॰) प्रत्यक्ष रूप से और एक ही समय में इमाम मालिक (रह॰) के भी शिष्य हैं और इमाम मुहम्मद के भी। दूसरी तरफ़ इमाम अबू-यूसुफ़ ने इमाम मालिक (रह॰) से ज्ञान प्राप्त किया। फिर इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) सीधे इमाम शाफ़िई (रह॰) के शिष्य हैं। इस तरह से इमाम मालिक (रह॰) का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनसे चारों बड़े फ़िक़ही मसलकों का वास्ता रहा और यह सब आकर किसी-न-किसी तरह से उनके व्यक्तित्व पर जमा हो गए।
यों मुवत्ता इमाम मालिक का महत्व हदीस की एक किताब की दृष्टि से तो है ही, लेकिन फ़िक़्ह की किताब की दृष्टि से भी इसकी एक अलग हैसियत और महत्व यह है कि इसमें बड़े सहाबा और ताबिईन के साथ-साथ इमाम मालिक (रह॰) के अपने इज्तिहादात भी मौजूद हैं। इस दृष्टि से भी इसका महत्व है कि यह वह किताब है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तमाम मसलकों के लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है। मुवत्ता इमाम मालिक तमाम फ़िक़ही मसलकों में पढ़ाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के हर मदरसे में, चाहे वह किसी भी मसलक का हो, मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ाई जाती है। गोया यह वह किताब है जो मुसलमानों के हर मसलक के लोगों में, चाहे वे हनफ़ी हों, मालिकी हों, हंबली और शाफ़िई हों यहाँ तक कि ग़ैर-सुन्नी मसलकों मसलन ज़ैदी मसलक में भी मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ाई जाती है।
मुवत्ता इमाम मालिक की इतनी व्याख्याएँ लिखी गई हैं कि उनकी संख्या सैंकड़ों में है। मालकियों और ग़ैर-मालकियों सबने, बल्कि हर प्रकार के लोगों ने मुवत्ता पर काम किया। मुवत्ता का उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, फ़ारसी और कई एक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है।
मुवत्ता इमाम मालिक के साथ-साथ, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो किताब फ़िक़्हे-मालिकी के आधार की हैसियत रखती है वह ‘किताबुल-मुदव्वना’ है। इसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। ‘मुदव्वना’ इमाम मालिक (रह॰) के एक प्रत्यक्ष शिष्य और प्रसिद्ध इस्लामी मुजाहिद क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात ने संकलित की थी। वह इमाम मालिक (रह॰) के शिष्यों में क़रीब-क़रीब वही दर्जा रखते हैं जो इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी को इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के शिष्यों में प्राप्त है। क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात जब इमाम मालिक (रह॰) के दर्स में बैठते थे तो उनकी रायों और इज्तिहादात को हाथ-के-हाथ लिखते रहते थे। जहाँ-जहाँ इमाम मालिक (रह॰) से पूछते थे वह भी लिखते थे कि मैंने यह पूछा तो उन्होंने यह जवाब दिया। मैंने जवाब में यह कहा तो उन्होंने यह कहा। कुछ स्थानों पर कई-कई पृष्ठों तक क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात और इमाम मालिक (रह॰) की चर्चा चल रही है कि मैंने यह कहा और जवाब में इमाम मालिक (रह॰) ने यह फ़रमाया। आख़िर में इमाम मालिक (रह॰) ने कहा कि तुम ठीक कहते हो या फिर आख़िर में क़ाज़ी असद ने बताया कि आप ठीक कहते हैं। या यह कि इमाम मालिक (रह॰) ने आख़िर में कहा कि मैं अपनी बात पर क़ायम हूँ। और क़ाज़ी असद ने कहा कि मैं अपनी बात पर क़ायम हूँ।
ये थे क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात जिनकी एक विशेषता बड़ी अजीबो-ग़रीब है। वह यह है कि क़ाज़ी असद फ़क़ीह और क़ाज़ी होने के साथ-साथ एक इस्लामी योद्धा और सिपहसालार भी थे। सिसली में जब मुसलमान फ़ौजें गईं तो जिन विजेताओं के हाथों सिसली द्वीप फ़त्ह हुआ उनमें क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात भी शामिल हैं। यह क़लम के भी धनी थे और तलवार के भी माहिर। दूसरी विशेषता उनकी यह है कि उन्होंने इमाम मालिक (रह॰) के साथ-साथ इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी से भी ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से इमाम मुहम्मद की शैली या इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की methodology और इमाम मालिक (रह॰) की methodology दोनों को उन्होंने एक-दूसरे के साथ मिलाया और दोनों के तर्क करने के ढंग को इकट्ठा किया और वह किताब लिखी जो फ़िक़्हे-मालिकी की सबसे मौलिक किताब है। फिर जब फ़िक़्हे-मालिकी की यह मूल किताब लिखी जा चुकी तो इसको बहुत जल्द तमाम मालिकी हलक़ों में लोकप्रियता प्राप्त हो गई। कुछ समय के बाद क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात और उनके समकालीन कई दूसरे मालिकी फ़ुक़हा के शिष्य और एक माध्यम से इमाम मालिक (रह॰) के शिष्य इमाम अब्दुस्सलाम-बिन-सहनून तनूही ने कैरुआन में बैठकर इस किताब का नया एडिशन तैयार किया। इसमें बहुत-सी चीज़ों की वृद्धि की। क्रम को बेहतर बनाया और इसका नाम ‘अल-मुदव्वना’ रखा। इससे पहले यह किताब क़ाज़ी असद-बिन-फ़ुरात के ताल्लुक़ से ‘असदिया’ कहलाती थी। अब वही किताब ‘अल-मुदव्वनतुल-कुबरा’ कहलाती है जो सात या आठ भागों में हर जगह उपलब्ध है। इसमें इमाम मालिक (रह॰) के इज्तिहादात और कथनों के साथ-साथ जिनका यह सबसे बड़ा ख़ज़ाना है, कहीं-कहीं दूसरे फ़ुक़हा के कथन भी मिलते हैं।
फ़िक़्हे-मालिकी के महत्वपूर्ण ‘मुतून’
फ़िक़्हे-मालिकी में बहुत-से ‘मुतून’ लिखे गए जिनकी तफ़सील बयान करने के लिए ख़ासा तवील समय दरकार होगा। उनमें दो तीन प्रसिद्ध ‘मुतून’ के बारे में कुछ बताता हूँ। फ़िक़्हे-मालिकी का सबसे महत्वपूर्ण ‘मत्न’ ‘मुख़्तसर अल-ख़लील’ है। अल्लामा ख़लील एक नामवर मालिकी फ़क़ीह थे। यह उनकी किताब है। यह ‘मत्न’ फ़िक़्हे-मालिकी में वही हैसियत रखता है जो फ़िक़्हे-हनफ़ी में ‘मुख़्तसर अल-क़ुदूरी’ को प्राप्त है। यह ‘मत्न’ अपने आरम्भ से तमाम मालिकी दर्सगाहों और ज्ञानपरक क्षेत्रों में एक लम्बे समय तक लोकप्रिय रहा। फ़िक़्हे-मालिकी की दर्जनों किताबें ‘मुख़्तसर अल-ख़लील’, की व्याख्या में लिखी गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ‘मुख़्तसर अल-ख़लील’ की लगभग तीन सौ व्याख्याएँ लिखी गईं हैं। ये व्याख्याएँ तीन सौ हैं या कम या ज़्यादा, जितनी भी हैं उनमें से अधिकतर आज या तो सिरे से उपलब्ध नहीं हैं या मख़तूतात (हस्तलिपियों) के रूप में हैं। अगरचे उस समय भी इस किताब की कई दर्जन व्याख्याओं के फ़ुटनोट या जाँच-पड़ताल प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं।
‘किताबुत्तलक़ीन फ़िल-फ़िक़्हुल-मालिकी’ एक और महत्वपूर्ण किताब है। यह क़ाज़ी अबू-मुहम्मद अब्दुल-वह्हाब बग़्दादी ने लिखी है। वे बग़दाद के रहनेवाले थे और पाँचवीं सदी हिजरी में तमाम मालिकी फ़ुक़हा के सरदार कहलाते थे। उनको ‘शैख़ुलमालिकिया फ़ी अ-स्र’ कहा जाता था। उनकी यह किताब बड़ी प्रसिद्ध है और कई बार प्रकाशित हुई है। अल्लामा माज़री ने इसकी व्याख्या लिखी थी। इमाम माज़री के बारे में कहा जाता है कि उनके ज़माने में उनसे बड़ा कोई मालिकी फ़क़ीह नहीं था। इसके बाद फ़िक़्हे-मालिकी का एक और ‘मत्न’ है ‘अल-काफ़ी फ़ी फ़िक़्ह अहले-मदीना अल-मालिकी’। यह किताब अल्लामा इब्ने-अब्दुल-बर्र ने लिखी है जो अपने ज़माने में हाफ़िज़ अहले-मग़रिब कहलाते थे। यानी उलूमे-हदीस का उनसे बढ़कर कोई माहिर पश्चिमी जगत् में मौजूद नहीं था। स्पेन, पुर्तगाल, मराक़श, लीबिया अल-जज़ाइर और त्यूनीशिया के पूरे इलाक़े में सबसे बढ़कर हदीस के हाफ़िज़ अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने-अब्दुल-बर्र कहलाते हैं। उनकी बहुत-सी किताबें हैं जो अधिकतर इल्मे-हदीस पर हैं। लेकिन फ़िक़्हे-मालिकी पर उनका यह ‘मत्न’ बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने ‘अल-इस्तिज़कार’ और ‘अत्तमहीद’ के नाम से मुवत्ता इमाम मालिक की दो बड़ी व्याख्याएँ लिखीं। ये दोनों व्याख्याएँ मुवत्ता इमाम मालिक की महत्वपूर्ण तरीन शरहों (व्याख्याओं) में शुमार होती हैं।
फ़िक़्हे-मालिकी की इन किताबों के अलावा भी बहुत-सी और किताबें विभिन्न फ़िक़ही विषयों पर अलग-अलग लिखी गई हैं। उनमें से एक किताब जो पूरे फ़िक़ही साहित्य में अपनी कला की बेहतरीन किताब है, वह ‘तबसिरुल-हुक्काम’ है। यह अल्लामा इब्ने-फ़रहून ने लिखी है जो आठवीं सदी हिजरी के एक बड़े फ़क़ीह थे। यह इस्लाम के क़ानून संहिता पर अति व्यापक किताब है और फ़िक़्हे-इस्लामी के संग्रह में क़ानून संहिता पर इससे ज़्यादा अच्छी कोई और किताब मौजूद नहीं। फ़िक़्हे-मालिकी की शेष किताबों को मैं छोड़ता हूँ।
फ़िक़्हे-शाफ़िई
इसके बाद इमाम शाफ़िई (रह॰) की तरफ़ आते हैं। इमाम शाफ़िई (रह॰) इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) में अत्यन्त ऊँचा और अलग स्थान रखते हैं। मुस्लिम जगत् में इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के बाद जिस फ़क़ीह के माननेवालों की संख्या सबसे ज़्यादा है वे इमाम शाफ़िई (रह॰) हैं। उनको एक ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त है जो किसी और फ़क़ीह को कम ही प्राप्त हुआ होगा। वह यह कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के शिष्यों में कुछ ऐसे भी फ़ुक़हा शामिल हैं जो स्वयं अपनी जगह एक फ़िक़ही मसलक के संस्थापक थे। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) के शिष्यों में कोई फ़िक़ही मसलक का ख़ुद से संस्थापक नहीं हुआ, लेकिन इमाम शाफ़िई (रह॰) के शिष्यों में अनेक नामवर लोग अपने-अपने फ़िक़ही मसलक के संस्थापक हुए। इमाम अहमद-बिन-हंबल, इमाम दाऊद ज़ाहिरी, अबू-सौर बग़्दादी, अबू-जाफ़र-बिन-जरीर तबरी और कई दूसरे लोग, जिनसे आगे चलकर अलग-अलग फ़िक़ही मसलक बने, वह इमाम शाफ़िई (रह॰) के प्रत्यक्ष शिष्यों में से हैं।
किताबुल-उम्म
फ़िक़्हे-शाफ़िई की जो अस्ली किताब है वह ‘किताबुल-उम्म’ है। इसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। यह इमाम शाफ़िई (रह॰) की बहुत-सी किताबों का संग्रह है। आप कह सकते हैं कि यह इमाम शाफ़िई (रह॰) की complete works की हैसियत रखती है। इमाम शाफ़िई (रह॰) ने विभिन्न फ़िक़ही विषयों पर जितनी किताबें लिखीं यह उन सबका संग्रह है। जो इमाम शाफ़िई (रह॰) के आख़िरी दौर के इज्तिहादात पर आधारित है। इमाम शाफ़िई (रह॰) के पहले दौर के इज्तिहादात इस किताब में नहीं हैं, बल्कि दूसरे दौर के इज्तिहादात इस किताब में मौजूद हैं। यह किताब आठ मोटी जिल्दों में है और एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है। किसी और फ़िक़ही मसलक के संस्थापक के अपने क़लम से लिखी हुई इतनी व्यापक कोई और किताब मौजूद नहीं है जो इतनी असाधारण अन्तर्दृष्टि और इतने मज़बूत तर्कों पर आधारित हो। जब कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ता है तो इमाम शाफ़िई (रह॰) की तर्क-शक्ति के सामने बहता चला जाता है। कुछ जगहों पर जहाँ इमाम शाफ़िई (रह॰) ने इमाम मालिक (रह॰) के साथ अपनी वार्ता उद्धृत की है, उस वार्ता बल्कि ज्ञानपरक परिचर्चा में जब पढ़नेवाला इमाम शाफ़िई (रह॰) की बात पढ़ता है तो उनकी बात का समर्थक होता जाता है और यह समझता है कि इससे आगे तो कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जब इमाम मालिक (रह॰) का जवाब पढ़ता है तो ख़याल होता है कि इससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसी तरह जब इमाम शाफ़िई (रह॰) और इमाम मुहम्मद की परिचर्चा पढ़ता है तो दोनों का दृष्टिकोण बड़ा मज़बूत मालूम होता है। छोटे-से-छोटे मसले पर जब इमाम शाफ़िई (रह॰) की बात पढ़ता है तो मालूम होता है कि यह मसला तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसपर इतना ही ग़ौर करना चाहिए था। गोया ‘किताबुल-उम्म’ न केवल फ़िक़्हे-शाफ़िई की, बल्कि पूरी मानव जगत् के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण किताब है जिसको पूरी मानव जाति की साझी विरासत क़रार दिया जाना चाहिए। अगर ग़ैर-मुस्लिम अपने दुर्भाग्यवश इसको अपनी विरासत क़रार न दें तो यह उनका दुर्भाग्य है। उनको अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से यह मुसलमानों की एक अत्यन्त सम्माननीय विरासत है जो पूरे मानव जगत् और मुस्लिम जगत् के लिए गर्व का कारण है।
फ़िक़्हे-शाफ़िई के ‘मुतून’
फ़िक़्हे-शाफ़िई में भी बहुत-से ‘मुतून’ लिखे गए। सबसे लोकप्रिय मत्न ‘अल-मज़हब फ़िल-फ़िक़्हिश-शाफ़िई’ है। इसको इमाम अबू-इसहाक़ शीराज़ी ने संकलित किया था। यह वैसे तो दो भागों में है और अगर कोशिश की जाए तो एक भाग में भी आ सकता है। इसमें चौथी या पाँचवीं सदी हिजरी के आरम्भ तक फ़िक़्हे-शाफ़िई में जितने इज्तिहादात और समस्याएँ संकलित हुई थीं उन सबका सार समो दिया गया है। इसकी कई शरहें (व्याख्याए) लिखी गई हैं जो अपने-अपने समय में लोकप्रिय हुईं, लेकिन एक व्याख्या जो आज तक बहुत लोकप्रिय और मारूफ़ है वह ‘किताबुल-मजमूअ’ के नाम से हर जगह उपलब्ध है और लगभग बीस-बाईस भागों में है। आधी इमाम नववी ने लिखी थी जिनके नाम, स्थान, रुत्बे और ज्ञानपरक कारनामों से हदीस का हर विद्यार्थी परिचित है। आपने ‘रियाज़ुस्सलिहीन’ और ‘अरबईने-नववी’ का नाम निश्चय ही सुना होगा। ये दोनों अत्यन्त लोकप्रिय किताबें इमाम नववी ही की संकलित की हुई हैं। सम्भवत: किसी और ‘अरबईन’ या ‘चहल-हदीस’ को इतनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई जितनी इमाम नववी की इस ‘अरबईन’ को प्राप्त हुई। यह इमाम नववी शाफ़िई मसलक के माननेवाले थे। बड़े मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा में से थे। और अजीब संयोग की बात यह है कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के मज़ार के क़रीब ही इनका भी मज़ार है। मुझे कई बार इमाम शाफ़िई (रह॰) के मज़ार पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर बार इमाम नववी के मज़ार पर भी हाज़िरी नसीब हुई। ‘किताबुल-मजमूअ फ़ी शरहिल-मुहज़्ज़ब’ आधी इमाम नववी की लिखी हुई है और आधी अल्लामा तक़ीउद्दीन सुबकी ने लिखी है।
फ़िक़्हे-शाफ़िई की एक और किताब जो बड़ी प्रसिद्ध है वह ‘अल-हावी अल-कबीर’ है। यह बौद्धिक किताब अल्लामा मावर्दी की लिखी हुई है। अल्लामा अबुल-हसन मावर्दी अपने दौर के बहुत बड़े फ़क़ीह और अब्बासी साम्राज्य के चीफ़ जस्टिस थे। उनकी प्रसिद्ध किताब ‘अल-अहकामुस्सुल्तानिया' से हममें से बहुत-से लोग परिचित हैं। उन्होंने बहुत-से भागों में एक विस्तृत किताब लिखी थी। इसके कुछ भाग प्रकाशित हुए हैं और कुछ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसका एक अध्याय जो ‘अदबुल-क़ाज़ी’ पर था वह दो मोटे भागों में आज से पंद्रह बीस वर्ष पहले बग़दाद में प्रकाशित हुआ था। शेष किताब के भी कुछ भाग प्रकाशित हुए हैं और कुछ का प्रकाशित होना अभी बाक़ी है। फ़िक़्हे-शाफ़िई की दो मज़ीद उल्लेखनीय किताबों में से एक ‘मुग़नियुल-मुहताज’ है जो अल्लामा ख़तीब शिरबीनी की रचना है और दूसरी शाफ़िई मत्न की व्याख्या है। दूसरी किताब अल्लामा रमली ने लिखी है जिनको अपने ज़माने में शाफ़िई सग़ीर (छोटे इमाम शाफ़िई) कहा जाता था। उन्होंने ‘निहायतुल-मुहताज’ के नाम से किताब लिखी है। ये दो किताबें मुताख़्ख़िरीन (बादवाले फ़ुक़हा) के यहाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं और फ़िक़्हे-शाफ़िई की बड़ी महत्वपूर्ण किताबें शुमार होती हैं। फ़िक़्हे-शाफ़िई की किताबें तो ज़ाहिर है कि सैंकड़ों, बल्कि हज़ारों की संख्या में हैं। इन सबका सीमित समय में विस्तृत विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है।
फ़िक़्हे-हंबली
फ़िक़्हे-हंबली का आधार जिन किताबों पर है वे स्वयं इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) की लिखी हुई तो नहीं हैं, क्योंकि इमाम अहमद (रह॰) ने फ़िक़्ह पर कोई किताब नहीं लिखी। लेकिन उन्होंने मुस्नदे-इमाम अहमद के नाम से हदीस का एक बहुत बड़ा संग्रह संकलित किया था। इसमें जो हदीसें बयान हुई हैं, इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) अधिकतर उन्ही हदीसों के आधार पर फ़तवे दिया करते थे। लेकिन इमाम अहमद (रह॰) के फ़तवे जो इन हदीसों की समझ पर या उनकी व्याख्या पर आधारित होते थे, वे उनके कई शिष्यों ने संकलित किए। उन शिष्यों में एक इमाम अबू-बक्र अल-असरम और एक अब्दुल्लाह अल-ख़िलाल थे। इन दोनों की किताबें फ़िक़्हे-हंबली के आधार हैं। आज भी मिलती हैं और हर दौर में हंबली फ़ुक़हा ने इन दो किताबों के आधार पर फ़तवे जारी किए।
फ़िक़्हे-हंबली के महत्वपूर्ण ‘मुतून’
फ़िक़्हे-हंबली के बहुत-से ‘मुतून’ विभिन्न सदियों में लिखे गए। उनमें जो महत्वपूर्ण मुतून हैं वे तीन हैं। एक अल्लामा अबुल-क़ासिम ख़िरक़ी का ‘मत्न’ है जो ‘अल-मुख़्तसर फ़िल-फ़िक़्ह’ कहलाता है जिसको संक्षेप में ‘मुख़्तसर अल-ख़िरक़ी’ कहते हैं। यह तीन हज़ार दो सौ ‘मसाइल’ (समस्याओं) पर सम्मिलित है जो फ़िक़्हे-हंबली के मूल और अति प्रमाणित ‘मसाइल’ में से हैं। यह ‘मत्न’ आरम्भ ही से एक लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक की हैसियत से हर जगह लोकप्रिय एवं परिचित है। ‘मुख़्तसर अल-ख़िरक़ी’ फ़िक़्हे-हंबली का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ‘मत्न’ है। फ़िक़्हे-हंबली में इसकी वही हैसियत है जो फ़िक़्हे-हनफ़ी में ‘मुख़्तसर अल-क़ुदूरी’ की है, बल्कि यह कहा जाए तो शायद ग़लत न होगा कि ख़िरक़ी का ‘मत्न’ कई दृष्टि से क़ुदूरी से ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए कि जितनी बड़ी संख्या में इसकी व्याख्याएँ लिखी गईं उतनी संख्या में ‘मुख़्तसर क़ुदूरी’ की शरहें नहीं लिखी गईं। कुछ हंबली फ़ुक़हा का बयान है कि ‘मुख़्तसर ख़िरक़ी’ पर लिखी जानेवाली व्याख्याओं की संख्या तीन सौ के लगभग है। कुछ विद्वानों ने छात्रों की सुविधा की ख़ातिर उसको नज़्म भी किया है। कुछ लोगों ने इसके शब्दकोष की व्याख्या पर भी किताबें लिखी हैं।
‘मुख़्तसर अल-ख़िरक़ी’ की व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध अल्लामा मूफ़िक़ुद्दीन अबू-मुहम्मद अब्दुल्लाह-बिन-अहमद इब्ने-क़ुदामा (मृत्यु 620 हि॰) की व्याख्या है जो तेरह-चौदह भागों में अल-मुग़नी के नाम से बार-बार प्रकाशित हो चुकी है और सऊदी अरब की हुकूमत की दिलचस्पी और लगन से विस्तृत पैमाने पर वितरित की जाती रही है। किताब के लेखक अल्लामा इब्ने-क़ुदामा अपने ज़माने के अत्यन्त नामवर हंबली फ़ुक़हा में से थे। उनको बचपन ही से ‘मुख़्तसर अल-ख़िरक़ी’ से दिलचस्पी रही। उन्होंने यह किताब कंठस्थ भी कर ली थी।
अल्लामा इब्ने-क़ुदामा फ़िक़्ह के साथ-साथ तज़किया-ए-नफ़्स (मन को शुद्ध करने) और आध्यात्मिकता में भी उच्च स्थान रखते थे। बग़दाद में जहाँ वे कई वर्ष रहे, उन्होंने शैख़ अब्दुल-क़ादिर जीलानी (रह॰) से भी ज्ञान प्राप्त किया।
अल्लामा इब्ने-क़ुदामा ने यों तो बहुत-सी किताबें लिखीं जिनमें से चालीस-पैंतालीस किताबों का उल्लेख अल-मुग़नी के शोधकर्ताओं ने किताब के मुक़द्दमे में किया है, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक रचना अल-मुग़नी ही है जो फ़िक़्हे-इस्लामी के पूरे लिटरेचर में बहुत उच्च स्थान रखती है, बल्कि यह कहना ग़लत न होगा कि अल-मुग़नी की गिनती फ़िक़्हे-इस्लामी की कुछ बेहतरीन और अति लाभदायक किताबों में होती है। इस किताब की हैसियत एक ऐसे इंसाइक्लोपीडिया की है जिसमें फ़िक़्ह के तुलनात्मक अध्ययन से काम लिया गया है और हर महत्वपूर्ण फ़िक़ही मसले के बारे में विभिन्न फ़ुक़हा और फ़िक़ही मसलकों का दृष्टिकोण और उनके तर्क विस्तार से बयान हुए हैं। किताब का अंदाज़ अत्यन्त संकलित और मंतिक़ी और शैली अत्यंत स्पष्ट और सरल है। इस किताब के अध्ययन से न केवल प्रतिष्ठित फ़ुक़हा के इज्तिहादात और उनके तर्कों को समझने में सहायता मिलती है, बल्कि पाठकों को एक गहरी अन्तर्दृष्टि भी प्राप्त होती है।
अल-मुग़नी पूरे फ़िक़ही भंडार की कुछ बेहतरीन किताबों में से एक है। अगर आप मुझसे कहें कि फ़िक़्हे-हंबली की बेहतरीन किताब का चयन करो तो मैं अल-मुग़नी का चयन करूँगा। जिस तरह फ़िक़्हे-हनफ़ी की बेहतरीन किताब ‘बदाइउस्सनाइअ’ होगी। इसी तरह से फ़िक़्हे-हंबली की बेहतरीन किताब अल-मुग़नी है और यह कई हवालों से ‘बदाए’ से बेहतर है। ‘बदाइउस्सनाइअ’ में शेष फ़ुक़हा की रायों से ज़्यादा बहस नहीं की गई है, लेकिन अल-मुग़नी में तमाम फ़ुक़हा की रायों से बहस की गई है। अगर किसी के पास अल-मुग़नी हो तो उसको मालूम हो जाएगा कि किसी मामले में शेष फ़ुक़हा का दृष्टिकोण क्या है। यह एक ऐसी चीज़ है जो इसको कई दूसरी किताबों से अलग करती है।
फ़िक़्हे-हंबली का दूसरा मत्न ‘अल-उम्दा फ़िल-फ़िक़्हिल-हंबली’ कहलाता है। यह भी उन्हीं अल्लामा इब्ने-क़ुदामा की रचना है। ‘अल-उम्दा’ का अंदाज़ फ़िक़्हुस्सुन्नः या फ़िक़्हुल-हदीस की किताबों का-सा है। यह किताब आदेशों से सम्बन्धित हदीसों का एक अच्छा संग्रह है। अगरचे ‘अल-उम्दा’ इस अंदाज़ का ‘मत्न’ तो नहीं है जिस अंदाज़ के ‘मुतून’ अल्लामा ख़िरक़ी और अल्लामा क़ुदूरी वग़ैरा के हैं, लेकिन चूँकि बतौर एक पाठ्य पुस्तक के इसकी लोकप्रियता अन्य ‘मुतून’ की तरह ही रही है इसलिए इसको भी फ़िक़ही ‘मुतून’ के साथ ज़िक्र किया जाता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि दूसरे फ़िक़ही मसलकों में ‘अल-उम्दा’ के अंदाज़ की कोई पाठ्य पुस्तक इतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी लोकप्रियता सर्वोच्च अल्लाह ने ‘अल-उम्दा’ को प्रदान की। ‘अल-उम्दा’ की कई शरहें लिखी गईं। उनमें से एक ‘अल-उम्दा फ़ी शरहिल-उम्दा’ चार भागों में है जो प्रसिद्ध है और कई बार प्रकाशित हुई है। यह किताब भी सऊदी अरब हुकूमत के प्रबन्धन से दुनिया-भर में विस्तृत पैमाने पर विततिरत की गई है इसलिए हर बड़े पुस्तकालय में उपलब्ध है। तीसरा मत्न ‘अल-मुक़न्ना’ है जो फ़िक़्हे-हंबली में प्रसिद्ध है। ‘अल-मुक़न्ना’ भी अल्लामा इब्ने-क़ुदामा ही की रचना है जो फ़िक़्ह के मध्यम दर्जे के छात्रों के लिए लिखी गई है। अल्लामा इब्ने-क़ुदामा ने फ़िक़्ह के विभिन्न दर्जों के छात्रों के लिए ‘अल-उम्दा’, ‘अल-मुक़न्ना’ और ‘अल-काफ़ी’ के नाम से तीन ‘मुतून’ तैयार किए। ‘अल-मुक़न्ना’ की एक व्याख्या ‘अश-शरहुल-कबीर’ के नाम से लिखी गई है जो शम्सुद्दीन-बिन-क़ुदामा ने लिखी है। मूफ़िक़ुद्दीन-बिन-क़ुदामा की अल-मुग़नी और शम्सुद्दीन-बिन-क़ुदामा की ‘अश-शरहुल-कबीर, ये दोनों शरहें फ़िक़्हे-हंबली में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
फ़िक़्हे-हंबली के दो महत्वपूर्ण मुजद्दिद
फ़िक़्हे-हंबली के दो जलीलुल-क़द्र मुजद्दिद आठवीं सदी में गुज़रे हैं जिन्होंने फ़िक़्हे-हंबली को नई धारणाओं, नए विचारों और नए इज्तिहादात से माला-माल कर दिया और नई रूह से इसमें एक नया जीवन पैदा कर दिया। ये दोनों ऐसे फ़ुक़हा थे जिनके बिना फ़िक़्हे-हंबली तो क्या, फ़िक़्हे-इस्लामी का इतिहास भी पूरा नहीं हो सकता, यानी अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) और उनके शिष्य अल्लामा इब्ने-क़य्यिम (रह॰)। अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) के फ़तवे मात्र फ़तवे नहीं हैं, बल्कि कुछ विषयों पर बाक़ायदा किताबें हैं। यह फ़तवे चालीस भागों में कई बार छपे हैं और लगभग हर इस्लामी पुस्तकालय में मौजूद हैं। फ़िक़्हे-हंबली अल्लामा इब्ने-तैमिया के फ़तवों से अलग नहीं हो सकती। न केवल फ़िक़्हे-हंबली, बल्कि फ़िक़्हे-इस्लामी के ज़ख़ीरे में जो फ़तवे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनमें से अल्लामा इब्ने-तैमिया के फ़तवे भी हैं।
अल्लामा इब्ने-तैमिया के शिष्य इब्ने-क़य्यिम की किताब ‘आलामुल-मौक़ऐन’ शरीअत की तत्वदर्शिता और फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह की साझा समस्याओं पर असाधारण और बड़े निराले प्रकार की किताब है। शेष विवरण मैं छोड़ देता हूँ। फ़िक़्हे-हंबली में और भी बहुत सारे ‘मुतून’ हैं। समय की तंगी के कारण उनका उल्लेख मुश्किल है। ‘अल-फ़ुरूअ’ और ‘ज़ादुल-मुस्तक़ना’ भी उल्लेखनीय हैं। ‘किताबुल-मुग़नी’ जिसका अभी मैंने ज़िक्र किया उसके बारे में सुल्तानुल-उलमा अल्लामा इज़ुद्दीन सलमी ने, जो स्वयं शाफ़िई मसलक के माननेवाले थे, यह लिखा है कि किताबुल-मुहल्ला और किताबुल-मुग़नी दोनों किताबें इस्लामी पुस्तकालयों के भंडार में अद्वितीय किताबें हैं। अपने सही क्रम की दृष्टि से, शोध लेख और उसमें दर्ज सामग्री की दृष्टि से उनका कोई जवाब नहीं।
फ़िक़्हे-ज़ाहिरी
एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण किताब जिसका मैं अन्य फ़िक़्ही मसलकों के उल्लेख के बाद ज़िक्र करना चाहूँगा, वह फ़िक़्हे-ज़ाहिरी के मुजद्दिदे-आज़म अल्लामा इब्ने-हज़्म की किताब है। अल्लामा इब्ने-हज़्म का सम्बन्ध चारों फ़िक़ही मसलकों में से किसी एक के साथ भी नहीं था। वे इमाम शाफ़िई (रह॰) के शिष्य इमाम दाऊद ज़ाहिरी की फ़िक़्हे-ज़ाहिरी के अनुयायी थे। इमाम दाऊद ज़ाहिरी की एक दो किताबें थीं जो हम तक नहीं पहुँचीं, लेकिन इस फ़िक़्ह का संकलन और नवीनीकरण अल्लामा इब्ने-हज़्म ने कर दिया। उनकी दो किताबें प्रसिद्ध हैं। एक ‘किताबुल-अहकाम फ़ी उसूलिल-अहकाम’ है जो उसूले-फ़िक़्ह पर है और दूसरी ‘किताबुल-मुहल्ला’ आठ दस मोटी जिल्दों में है। कई बार प्रकाशित हुई है और फ़िक़्हे-इस्लामी की सबसे महत्वपूर्ण फ़िक़ही किताबों में से एक है। यह किताब कई दृष्टि से फ़िक़्हे-इस्लामी की कुछ अत्यन्त उच्च कोटि की किताबों में शामिल किए जाने के योग्य है। अपनी भाषा-शैली, तार्किक शक्ति और समीक्षा एवं विश्लेषण की उत्कृष्टता के साथ-साथ भाषा और बयान की तेज़ी तथा ‘शाज़ अक़्वाल’ (अल्पमतों) की अधिकता की वजह से अल्लामा इब्ने-हज़्म की यह किताब हर दौर में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्षों की दिलचस्पी का समान विषय रही है।
फ़तवों की किताबें
फ़िक़्ह की किताबों का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार फ़तवों की किताबें हैं। फ़तवों की किताबें सैंकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों की संख्या में हैं। उनके नाम लेने में भी ख़ासा समय लगेगा। फ़तावा इब्ने-तैमिया जिस तरह फ़िक़्हे-हंबली में बहुत नुमायाँ है, फ़तावा तातारख़ानिया और फ़तावा आलमगीरी फ़िक़्हे-हनफ़ी में नुमायाँ हैं। इस तरह के और फ़तावा शेष मसलकों में प्रसिद्ध हैं।
अतीत निकट में एक महत्वपूर्ण किताब फ़िक़्हे-हनफ़ी में मुजल्लतुल-अहकामिल-अदलिया थी जो उसमानी साम्राज्य में एक संकलित क़ानून के तौर पर संकलित हुई और उसकी दर्जनों व्याख्याएँ लिखी गईं। एक ज़माना था 1875-76 से लेकर और 1944-45 तक, कि मुजल्लतुल- अहकामिल-अदलिया का राज मुस्लिम जगत् के बहुत बड़े हिस्से पर था। इस किताब की व्याख्याएँ लिखी गईं। तुर्की भाषा में, अरबी और उर्दू भाषा में इसकी कई व्याख्याएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। इस किताब का एक अलग इतिहास है। यह मुस्लिम जगत् में फ़िक़्ह के इतिहास में पहली किताब थी। जिसपर कल तफ़सील से बात करेंगे। जो बतौर एक संकलित क़ानून के लागू की गई और एक लम्बे समय तक लागू रही। फिर तुर्की में जब मुस्तफ़ा कमाल ने ख़िलाफ़त और शरीअत दोनों को निरस्त करके सेक्युलरिज़्म लागू किया तो इस क़ानून को भी निरस्त कर दिया। लेकिन शेष देशों में फिर भी यह किताब फ़िक़्हे-हनफ़ी की एक महत्वपूर्ण किताब के तौर पर लोकप्रिय रही। यह फ़िक़्हे-हनफ़ी के आधार पर दीवानी क़ानून के आदेश का एक प्रमाणित संग्रह है।
फ़िक़्ह का तुलनात्मक अध्ययन
एक आख़िरी चीज़ जिसको मैं एक दो जुमलों में कहना चाहूँगा वह ‘अल-फ़िक़्हुल-मक़ारिन’ या ‘फ़िक़्ह अलल-मज़ाहिब’ है। इस विषय पर किताबों का एक सिलसिला लिखा गया जिसमें तमाम फ़िक़्हों का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट था। इसमें सबसे पहली और अति महत्वपूर्ण किताब स्पेन के अल्लामा इब्ने-रुश्द ने ‘बदाइउल-मुज्तहिद’ के नाम से लिखी। यह फ़िक़्हे-इस्लामी की बेहतरीन किताबों में से है और अगर आपको मौक़ा मिले तो इस किताब को किसी उस्ताद से ज़रूर पढ़ें। मुझे नहीं पता कि मेरी बात को कितना महत्व दिया जाएगा, लेकिन मैं मश्वरा दूँगा कि इस किताब के कुछ हिस्से तमाम दीनी तालीमी संस्थाओं के कोर्स में ज़रूर शामिल किए जाएँ। यह तमाम फ़िक़ही मसलकों का एक तुलनात्मक अध्ययन है। इस किताब का एक बेहतरीन अंग्रेज़ी अनुवाद मेरे एक दोस्त ने किया है, अमेरिका में छपा है। ग़रज़ यह एक बेहतरीन किताब है जो फ़िक़्ह के विशेष छात्रों के लिए एक अपरिहार्य किताब है।
‘फ़िक़्हुल-मक़ारिन’ पर दूसरी महत्वपूर्ण किताब यमन में एक ज़ैदी फ़क़ीह ने लिखी थी ‘अलबहरुज़-ज़ख़ाइर अल-जामेउल-मज़ाहिब अल-उलमाउल-अबसार’। जितने फ़िक़ही मसलक हैं उन सबके दृष्टिकोण का एक तुलनात्मक अध्ययन। इसका नाम उन्होंने ‘अल-बहरुज़-ज़ख़्ख़ार’ रखा था। इसलिए कि इसमें नदी के-से प्रवाह के साथ फ़िक़ही समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इसी शैली की पैरवी में एक किताब बीसवीं सदी के शुरू में लिखी गई थी, ‘किताबुल-फ़िक़्ह अलल-मज़ाहिबिल-अरबआ’। इसमें चारों मसलकों का एक जायज़ा लिया गया है। इसका उर्दू अनुवाद भी उपलब्ध है जो पंजाब सरकार के वक़्फ़ विभाग ने कराया था। फिर एक और किताब लिखी गई थी ‘किताबुल-फ़िक़्ह अलल-मज़ाहिबिल-ख़मसा’। इसमें उन चार प्रसिद्ध सुन्नी मसलकों के साथ-साथ फ़िक़्हे-जाफ़रिया की भी वृद्धि की गई है।
अलबत्ता इस विषय की बेहतरीन किताब हमारे अत्यन्त विद्वान दोस्त और सीरिया के जाने-माने फ़क़ीह जो पिछले दिनों यहाँ आए भी थे, शैख़ वहबा अज़-ज़ुहैली की लिखी हुई है। ‘अल-फ़िक़्हुल-इस्लामी व-अदिल्लः’। यह बारह भागों में है। इसमें तमाम फ़िक़ही मसलकों का एक तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है। यह किताब इतनी व्यापक और इतनी बेहतरीन है कि इसने फ़िक़्हे-मक़ारिन की शेष सब किताबों को गोया पृष्ठभूमि में डाल दिया है। अब हर जगह यही किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है। यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शेष विवरण कल बयान होगा जो इंशाअल्लाह इस सिलसिले का आख़िरी प्रोग्राम होगा। मैं एक ही सवाल का जवाब दे सकता हूँ। इसलिए कि मुझे क्लास लेने जाना है और आज बात भी कुछ भी हो गई
सवालात
सवाल : What is Maslak in Figh? (फ़िक़्ह में मसलक किसे कहते हैं?)
जवाब : मसलक से मुराद वह है जिसको आप अंग्रेज़ी में school of thought यानी मकतबे-फ़िक्र कह सकते हैं। यानी इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने जब इज्तिहाद से काम लिया तो उन्होंने इज्तिहाद के कुछ उसूल बनाए। उन सिद्धान्तों को एक साइंटिफ़िक और संगठित या सिस्टमैटिक अंदाज़ में संकलित किया। इस सिस्टमैटिक और संकलित अंदाज़ की वजह से एक स्कूल ऑफ़ थॉट अस्तित्व में आया। इसको आप मसलक कह सकते हैं। जब इमाम शाफ़िई (रह॰) ने यह काम किया तो एक और मसलक अस्तित्व में आ गया। इमाम अहमद (रह॰) ने जब यह काम किया तो एक और मसलक अस्तित्व में आया। जब भी कोई बड़ा इस्लामी चिन्तक और बड़ा आलिम किसी ज्ञानपरक मसले पर सोचेगा तो वह छोटी-छोटी समस्याओं पर नहीं सोचेगा, बल्कि वह बड़ी-बड़ी समस्याओं को अपने चिन्तन-मनन का विषय बनाएगा और गोया एक विस्तृत और Macro लेवल पर सोचेगा और एक सिस्टम बनाएगा। इस सिस्टम के तैयार करने से स्कूल ऑफ़ थॉट आपसे-आप अस्तित्व में आ जाता है। यह इंसानी सोच की विशेषता है और वैचारिकता की एक अनिवार्य अपेक्षा है कि ऐसा अवश्य होगा। इसको मसलक कहते हैं।
✩
सवाल : What are Nusoos? (‘नुसूस’ किसे कहते हैं?)
जवाब : स्पष्ट आदेशों से मुराद है पवित्र क़ुरआन और हदीस का ‘मत्न’ (Text) क़ुरआन की आयत को ‘नस्स’ कहते हैं और हदीस को ‘नस्स’ कहते हैं। ‘नस्स’ का बहुवचन ‘नुसूस’ है।
✩
सवाल : If there are four Imams, how should we go about deriving modles of actions from at them? should we just adopt one? (यदि चार इमाम हैं, तो हमें उनके आधार पर कार्य के मॉडल कैसे तैयार करने चाहिएँ? क्या उनमें से एक को चुन लेना चाहिए?)
जवाब : बेहतर तो यह है कि आप जो कुछ अभी तक करते रहे थे वही करते रहें और इसमें कोई नई चीज़ शुरू न करें। लेकिन अगर आप चाहें कि किसी एक फ़क़ीह की पैरवी करें तो बेहतर यह है कि फिर एक ही फ़क़ीह की पैरवी करें। इसका मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कोई आदमी अपनी पसंद-नापसंद से pick and choose का काम शुरू कर दे तो इससे शरीअत के उद्देश्य को नुक़्सान पहुँचने की सम्भावना रहेगी। इसलिए सावधानी का तक़ाज़ा यह है कि किसी एक ही फ़क़ीह की राय की पैरवी करें, लेकिन जो विद्वान हैं, उन्होंने ने पहले उसको अनिवार्य समझा न आज अनिवार्य समझते हैं। जब फ़तवा देना होता है तो वे देख लेते हैं कि अगर किसी ख़ास मसलक का दृष्टिकोण ज़्यादा मज़बूत है तो उसके अनुसार वे फ़तवा दे देते हैं।
सवाल : ‘शरह’ की परिभाषा बता दीजिए!
जवाब : जिस तरह क़ानून की कमेंट्री होती है इसी तरह से विभिन्न ‘मुतून’ की कमेंट्रीज़ लिखी गईं। उनमें शब्दों की शरह (व्याख्या) की गई और उनको elaborate किया गया। इसका उदाहरण दिया गया, क्योंकि संक्षिप्त इबारत बहुत सटीक थी इसलिए उसकी व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई।
सवाल : हनफ़ी मसलक के कुछ लोगों का कहना कि जिसने किसी शाफ़िई इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं हुई और इसको नमाज़ दोहरानी चाहिए।
जवाब : फ़िक़्हे-इस्लामी में ऐसा कोई आदेश या उसूल नहीं है। जिसने भी ऐसा कहा है फ़ुज़ूल बात कही है और बिलकुल ग़लत कही है। जिस मसलक का इमाम नमाज़ पढ़ा रहा हो आप उसके पीछे बेफ़िक्र और बिना संकोच के नमाज़ पढ़ लें। अगर आज इमाम शाफ़िई (रह॰) यहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो मैं किसी आदमी को नमाज़ पढ़ाने नहीं दूँगा। स्वयं भी इमाम शाफ़िई (रह॰) के पीछे नमाज़ पढूँगा और दूसरों से भी यही कहूँगा कि वह इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ें। यह कहना कि इमाम शाफ़िई (रह॰) के पीछे मैं नमाज़ नहीं पढूँगा, यह अत्यन्त बदनसीबी है। इमाम शाफ़िई (रह॰) के इज्तिहादात हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इज्तिहादात पर आधारित हैं तो अगर अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) यहाँ तशरीफ़ लाएँगे तो कौन ऐसा बदतमीज़ और गुस्ताख़ होगा जो कहे कि मैं आपके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता। मेरे ख़याल में यह एक फ़ुज़ूल बात है। फ़िक़्हे-हनफ़ी के माननेवालों की नमाज़ फ़िक़्हे-शाफ़िई के माननेवालों के पीछे होती है। इसी तरह शाफ़िई (रह॰) की नमाज़ हनफ़ी के पीछे होती है। जो व्यक्ति कहता है कि दूसरे मसलक के इमाम के पीछे नमाज़ नहीं होती वह जाहिल भी है और नालायक़ भी।
LEAVE A REPLY
Cancel reply
Recent posts
-

फ़िक़्हे-इस्लामी आधुनिक काल में (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 12)
17 April 2025 -

इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 10)
23 March 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025
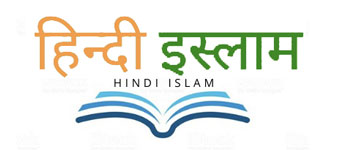
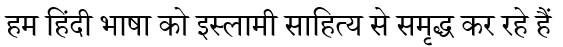
Comments
Abdul majid shaikh
Fiqah पर आधारित इस लेख को जो हिंदी लिपि में पढ़कर बड़ी खुशी हुई, काश इस लेख में मौजूद किताबें इसी तरह की लिपि में मौजूद होती तो ज्ञान भंडार में इजाफा किस कदर बढ़ जाता इस के लिए अल्फ़ाज़ मौजूद है सिर्फ इस मौजूद लेख से दिमाग में नई रोशनी जगह बनाई इसके लिए शुक्रिया. उम्मीद करते है कि आगे भी इस तरह की मालूमात इस तरह की लिपिमे पहुंचे तो गैर उर्दू पढ़ने वाले के इल्म में इजाफा ही होगा.