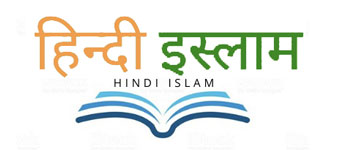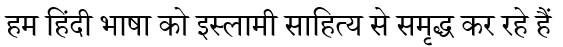इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 10)
-
फ़िक़्ह
- at 23 March 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक: गुलज़ार सहराई
लेक्चर नम्बर-10 (09 October 2004)
आज की चर्चा का शीर्षक है 'इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून'। फ़िक़्हे-इस्लामी का यह विभाग आधुनिक काल में वस्तुतः अत्यन्त महत्वपूर्ण क़रार दिया जाता है। इसलिए कि आधुनिक काल में इस्लामी आदेशों और क़ानूनों के लागू करने में जो मुश्किलें हैं वे सबसे ज़्यादा इस्लाम के व्यापार-क़ानून और मालियात के विभाग में पेश आ रही हैं। इसके बहुत-से कारणों में से महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यापार और वित्तीय व्यवस्था आधुनिक काल में बहुत जटिल हो गई है और इससे विभिन्न शक्तियों के अनगिनत हित जुड़ गए हैं। जब तक इन हितों को समाप्त करके अत्यन्त साहस, हिम्मत, स्वतंत्र रूप से और सकारात्मक सोच के साथ इन आदेशों को लागू नहीं किया जाएगा, उस समय तक शरीअत को लागू करने के मामले में पहल अत्यन्त जटिल और मुश्किल काम है।
आधुनिक काल की जटिल वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था
पिछले तीन सौ वर्षों के अन्तराल में पश्चिम के लोगों ने दुनिया के आर्थिक और वित्तीय मामलों के लिए एक ऐसी पेचीदा व्यवस्था का गठन किया है जिसका आधार ब्याज और ‘रिबा’ पर है। ब्याज और ‘रिबा’ की व्यवस्था को बढ़ावा देने, उसको परवान चढ़ाने और कुछ विशेष शक्तियों के हितों की पूर्ति करने के लिए पश्चिमी जगत् ने एक नई व्यवस्था का गठन किया है जिसको free market economy यानी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और आज़ाद मंडी की व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था का समर्थन और प्रचार बड़े लुभावने शब्दों, आकर्षक एलानों और प्रभावित करनेवाले दावों से किया जाता है। पूरा अर्थशास्त्र उस व्यवस्था की सेवा करने के लिए संकलित किया गया है। पूर्वी देशों के लोगों को अर्थशास्त्र, बैंकिंग और विकास एवं वित्त के मैदान में जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह इसी व्यवस्था की मौलिक धारणाओं और विचारों के अनुसार दिया जाता है। पूर्वी जगत् से आम तौर पर और मुस्लिम जगत् से विशेषकर पश्चिमी जगत् के सम्बन्ध जिस एक मूल बिन्दु पर क़ायम हैं वह इसी व्यवस्था की रक्षा और इसी व्यवस्था का प्रचार-प्रसार है।
इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि दुनिया के संसाधनों पर पश्चिमी शक्तियों का कंट्रोल बरक़रार रखा जाए, दुनिया की दौलत को ज़्यादा-से-ज़्यादा संकेन्द्रित किया जाए, तीसरी दुनिया के कच्चे माल को पश्चिमी देशों के उद्योगों और आर्थिक वर्चस्व के लिए प्रयुक्त किया जाए, तीसरी दुनिया की हैसियत पश्चिमी देशों की मंडियों से ज़्यादा न हो। इस पूरी स्थिति का परिणाम यह निकला है कि इस समय इस भू-भाग पर इंसानों को सर्वोच्च अल्लाह ने जो संसाधन प्रदान किए हैं, उनका 19 प्रतिशत दुनिया की 81 प्रतिशत आबादी के उपभोग में है। और उन संसाधनों के 81 प्रतिशत भागों पर इस समय दुनिया की 19 प्रतिशत आबादी का कंट्रोल है। ये आंकड़े भी लगभग दस वर्ष पहले के हैं और उनमें दिन-प्रतिदिन तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। पूर्वी दुनिया और मुस्लिम जगत् के संसाधन तेज़ी के साथ पश्चिमी दुनिया के कंट्रोल और प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं। आज पूर्वी जगत् को आम तौर से और मुस्लिम जगत् को विशेषकर इतनी भी आज़ादी उपलब्ध नहीं है कि वे अपने संसाधन को अपनी मर्ज़ी और अपने भविष्य की कल्पना के अनुसार प्रयोग कर सकें। मुस्लिम जगत् अपने संसाधन का कैसे उपयोग करे? मुस्लिम जगत् भौतिक विकास प्राप्त करना चाहे तो किस ढंग से करे? मुस्लिम जगत् अपने यहाँ आर्थिक न्याय व्यवस्था क़ायम करना चाहे तो किन दिशा निर्देशों पर करे? इन सब सवालों का जवाब पवित्र क़ुरआन और सुन्नत और मुसलमानों की वैचारिक और फ़िक़ही पूँजी से लेने की बजाय पश्चिमी धारणाओं और मानदंडों, बल्कि पश्चिम की इच्छाओं और निर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जा रहा है।
केवल यही नहीं, बल्कि इस्लाम के आदेशों और धारणाओं के बारे में बहुत-से शक-सन्देह और ग़लत-फ़हमियाँ पैदा की जा रही हैं। उनमें से कुछ सन्देहों का सम्बन्ध कम समझ से है। कुछ सन्देहों का सम्बन्ध इस्लामी दृष्टिकोण को सही ढंग से बयान न करने की वजह से है और कुछ का सम्बन्ध उन हितों से है जो पश्चिमी व्यवस्था से जुड़े हैं। इन परिस्थितियों में मुस्लिम जगत् के लिए यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून को सही तौर पर समझा जाए। उसकी तत्वदर्शिताओं की जानकारी पैदा की जाए। इसके उद्देश्य की समझ प्राप्त की जाए। उसकी कार्य-पद्धित के बारे में लोगों के ज़ेहन साफ़ हों और मौलिक धारणाओं से हर व्यक्ति अवगत हो।
एक-बार यह उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो आंशिक विवरणों का निर्धारण आसान है। आंशिक विवरणों में से बहुत-सी चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थितियों और समय को देखते हुए बदल सकती हैं। इसलिए आंशिक विवरणों की बहस में पड़ने के बजाय मुसलमानों का ध्यान फ़िल्हाल इस्लाम के इस्लामी वाणिज्यिक और वित्तीय क़ानून की तत्वदर्शिता, उद्देश्य, कार्य-पद्धति और मौलिक धारणाओं पर केन्द्रित रहना चाहिए। जब इन मामलों के बारे में फ़ैसला करनेवालों और पॉलिसी बनानेवालों का ज़ेहन साफ़ हो जाए तो फिर आंशिक विवरणों का निर्धारण बहुत आसान काम है और इसमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
फ़िक़्हे-इस्लामी : एक पूर्ण और संकलित व्यवस्था
जैसा कि इससे पहले कई बार बताया जा चुका है, फ़िक़्हे-इस्लामी एक पूर्ण व्यवस्था है। इसके तमाम अंग एक-दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि उनको एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक अंग के प्रभाव दूसरे अंगों पर और दूसरे अंगों के प्रभाव इस पहले अंग पर पड़ते हैं। यह सब अंग और अध्याय तार्किक रूप से एक-दूसरे के साथ पूरी तरह सम्बद्ध हैं। अगर किसी एक अंग को लागू किया जाए और शेष अंगों को अनदेखा कर दिया जाए तो उसके वे फल और लाभ प्राप्त नहीं होंगे जो पूरे तौर पर लागू करने और पूरे को अपनाने की स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। इस्लाम की व्यवस्था मौलिक रूप से एक नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामूहिक सतह पर इंसान का नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। परिवारों का प्रशिक्षण भी और संस्थाओं का प्रशिक्षण भी, समाजों का प्रशिक्षण भी और हुकूमतों का प्रशिक्षण भी, क़ानून का प्रशिक्षण भी और व्यवस्था का प्रशिक्षण भी। इन सब पहलुओं को नैतिक आचरण और अध्यात्म के दायरे में कैसे लाया जाए, अल्लाह की प्रसन्नता की ख़ातिर इंसान को जीवन गुज़राने का ढंग कैसे सिखाया जाए, यह इस्लाम का मौलिक उद्देश्य है। ज़ाहिर बात है व्यापार और वित्त इस्लाम के नज़दीक मानव-जीवन के बहुत-से विभागों में से एक विभाग है, सब कुछ नहीं है। मानव-जीवन के और भी बहुत-से पहलू और विभाग हैं। व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के अलावा भी इंसान की बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इंसानों की बहुत-सी व्यस्तताओं और बहुत-सी ज़िम्मेदारियों में से एक व्यापार भी है। उनमें से एक अर्थव्यवस्था भी है और एक वित्त भी है। लेकिन चूँकि अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्त से हर इंसान को वास्ता पड़ता है किसी को प्रत्यक्ष रूप से, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्त से सम्बन्धित आदेश किसी-न-किसी हद तक हर मुसलमान को मालूम होने चाहिएँ।
आप स्वयं व्यापारी न भी हों, लेकिन आपको व्यापारियों से वास्ता ज़रूर पड़ता है। प्रतिदिन आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए सौदा ख़रीदना पड़ता है। आपको स्वयं वित्त से चाहे कलात्मक रूप से वास्ता न पड़ता हो, लेकिन दूसरों से लेन-देन और व्यापार के लिए आपके पास धन होना चाहिए। आपको अर्थव्यवस्था में स्वयं दक्षता दरकार न हो, लेकिन जीवन की नित्य अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए अर्थव्यवस्था के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आपपर पड़ेंगे। इसलिए अर्थव्यवस्था की कुछ-न-कुछ जानकारी हर समय दरकार है और हर इंसान के लिए अपरिहार्य है। आज की बातों को उन बातों से मिलाकर पढ़ें और समझें जो इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाओं के बारे में बताई गई थीं तो बहुत-सी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि इस्लाम में धन की अवधारणा क्या है, मिल्कियत की परिकल्पना क्या है और धन और मिल्कियत में उपभोग के लिए शरीअत ने क्या सीमाएँ निर्धारित की हैं। वे बातें ज़रा ज़ेहनों में ताज़ा करें तो फिर बात आगे बढ़ेगी।
धन एवं स्वामित्व की इस्लामी अवधारणा
पवित्र क़ुरआन ने हर माल, हर सम्पत्ति और हर मिल्कियत का वास्तविक पैदा करनेवाला और मालिक सर्वोच्च अल्लाह को क़रार दिया है। इंसान उसका रखवाला है। आप इस क़लम, चश्मे और इस स्कार्फ़ के, जो आपके उपयोग में हैं, रखवाले हैं। मालिक अल्लाह है। मैं इस क़लम और शर्ट का, जो मेरे इस्तेमाल में हैं रखवाला हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का अस्ल और वास्तविक मालिक सर्वोच्च अल्लाह है। लेकिन सर्वोच्च अल्लाह ने इस शर्ट को मेरी मिल्कियत और इस स्कार्फ़ को आपकी मिल्कियत के तौर पर बयान किया है। इसी लिए पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह ‘अमवालुकम’ (तुम्हारे माल) और ‘अमवालुहुम’ (उनके माल) के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इससे इशारा मिलता है कि आभासी तौर पर आप चीज़ों के मालिक हैं और यह आपकी मिल्कियत हैं। इसलिए जो चीज़ आपकी मिल्कियत में समझी जाती है वह वास्तव में नहीं, बल्कि आभासी रूप से आपकी मिल्कियत है। गोया जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके प्रबन्ध और अमानत में दिया है, जिसका उपभोग करने में आप अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं, उससे लाभ उठाने का अधिकार केवल आपको है, किसी और को नहीं है। अब अगर मैं और आप इस बारे में कोई लेन-देन करना चाहें, मैं ख़रीदना चाहूँ, आप किराये पर देना चाहें या किसी और लेन-देन के परिणामस्वरूप उसकी मिल्कियत, या उसके लाभ या फल या परिणाम मुझे या किसी और को स्थानांतरित करने अभीष्ट हों, उसके लिए मौलिक निर्देश पवित्र क़ुरआन ने और कुछ ज़रूरी उसूल सुन्नत ने बयान किए हैं।
पवित्र क़ुरआन ने सैद्धान्तिक रूप से एक बात बताई कि “ऐ ईमान लानेवालो! अपस में एक-दूसरे के माल ग़लत तरीक़े से न खाओ — यह और बात है कि तुम्हारी आपस की रज़ामनदी से कोई सौदा हो।” (क़ुरआन, 4:29) जो तरीक़ा भी अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नापसन्द किया है वह ग़लत तरीक़ा है। इस तरीक़े से अगर माल खाओगे तो यह हराम है। सिवाय इसके कि व्यापार के ज़रिए एक-दूसरे से माल ले और दे सकते हो। और व्यापार भी वह जो आपस की पूरी रज़ामंदी के आधार पर हो। पवित्र क़ुरआन ने इस आयत में तीन उसूल बयान किए हैं जो इस्लाम के व्यापार-क़ानून की तीन मौलिक धाराएँ हैं। किसी का माल किसी भी ग़ैर-शरई और नाजायज़ तरीक़े से लेना जायज़ नहीं, बल्कि हराम है। हर वह तरीक़ा ग़लत है जिसकी शरीअत ने अनुमति न दी हो। ग़लत और हराम तरीक़े से किसी का माल लेना व्यक्ति, दल, गिरोहों और हुकूमत सबके लिए नाजायज़ है। इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) ने ‘किताबुल-ख़िराज’ में एक सिद्धान्त बयान किया है कि “हुकूमत के लिए यह बात बिलकुल जायज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति के जायज़ क़ब्ज़े से कोई चीज़ ले-ले सिवाय इसके कि वह एक साबित, तय-शुदा और जाने-माने हक़ के आधार पर हो।” केवल इस स्थिति में हुकूमत ले सकती है, इसके अलावा हुकूमत को कोई अधिकार नहीं कि आपको आपकी किसी सम्पत्ति से या जायज़ मिल्कियत से वंचित कर दे। जहाँ अनुमति दी गई है वहाँ भी कार्य-पद्धति और आदेश दिए गए हैं। अत: यह अनुमति न व्यक्ति को प्राप्त है और न राज्य को प्राप्त है। अगर किसी के साथ माल का लेन-देन करना हो तो इसका तरीक़ा केवल व्यापार और कारोबार है। व्यापार के अलावा और कोई तरीक़ा नहीं कि मैं आपके माल का मालिक बनूँ या आप मेरे माल के मालिक बनें। पवित्र क़ुरआन ने इस दो-तरफ़ा रज़ामंदी के बिना अनुमति नहीं दी, सिवाय इस स्थिति के कि मैं अपनी रज़ामंदी से कोई चीज़ आपको हिबा (भेंट) कर दूँ या तोहफ़ा दे दूँ, यह जायज़ है। लेकिन यह व्यापार या कारोबार नहीं कहलाएगा, इसलिए कि इसमें आपकी मर्ज़ी का कोई दख़ल नहीं है। यह मेरी एक-तरफ़ा मर्ज़ी होगी कि मैं कोई चीज़ आपको भेंट कर दूँ या आप कोई चीज़ किसी को भेंट कर दें।
आपसी सहमति (तराज़ी) का सिद्धान्त
इस्लाम के व्यापार-क़ानून की तीसरी धारा यह है कि जब व्यापार हो तो वह आपस की पूर्ण सहमति से हो। यहाँ पवित्र क़ुरआन ने ‘तराज़ी’ (आपसी सहमति) की शब्दावली प्रयुक्त की है। ‘तराज़ी’ का अर्थ है कि आप भी पूर्ण रूप से राज़ी हैं और वह भी पूर्ण रूप से राज़ी है। जब तक दोनों पक्षों की ओर से पूर्ण सहमति न हो, उस समय तक व्यापार जायज़ नहीं है।
अब ‘तराज़ी’ का सिद्धान्त तो पवित्र क़ुरआन ने बयान कर दिया। इस सिद्धान्त का और अधिक स्पष्टीकरण अनेक हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किया है। कभी-कभी इंसान यह महसूस करता है कि ‘तराज़ी’ मौजूद है। दोनों पक्ष राज़ी हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि दोनों तरफ़ से वास्तविक और सच्ची रज़ामंदी नहीं होती। एक व्यक्ति अत्यन्त परेशानी का शिकार है। उसकी माँ बीमार है, बाप मृत्यु शय्या पर है या सन्तान में से किसी को कोई फ़ौरी और महत्वपूर्ण आवश्यकता का सामना है, या स्वयं उसको इलाज के लिए लाखों रुपये दरकार हैं जो कहीं से उपलब्ध नहीं हैं। या कोई निकटतम सम्बन्धी मृत्यु शय्या पर है। इन परिस्थितियों में वह अपना घर या प्लाट बेचना चाहता है। अब अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो कि प्लाट या घर की क़ीमत बाज़ार में दस लाख है और वह उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए पाँच लाख में लेना चाहे तो यह ‘तराज़ी’ नहीं होगी। बज़ाहिर वह कहेगा कि हाँ जी मैं राज़ी हूँ। पूरी तरह से रज़ामंद हूँ आप दे दीजिए। इसलिए कि उसको तुरन्त पैसे चाहिएँ हैं। लेकिन वास्तव में यह ‘तराज़ी’ नहीं है। बेचनेवाले के लिए तो जायज़ है, क्योंकि वह मजबूर है। लेकिन ख़रीदार के लिए जायज़ नहीं है कि वह किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उसको बाज़ार से इतनी कम क़ीमत दे कि हर कोई उसको कम और अनुचित क़ीमत क़रार देगा।
इसी तरह से अगर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वीकृति व्यक्त करता है, लेकिन यह स्वीकृति उसने किसी ग़लत आभास के आधार पर दी है। उदाहरणार्थ आपने एक मकान बेच दिया जिसमें कृत्रिम छत लगी हुई है। लेकिन छत के ऊपर से कुछ और लगा हुआ है। जिससे पता नहीं चलता कि छत कृत्रिम है। आपने यह आभास दिया कि कृत्रिम छत के ऊपर लेंटर लगा हुआ है और छत मज़बूत सीमेंट की है। बाद में ख़रीदार को पता चला कि ऐसा नहीं है और छत लकड़ी की है। अब इस व्यक्ति को अधिकार है कि चाहे तो इस सौदे को निरस्त कर दे, क्योंकि उसका ख़याल था कि छत पक्की है और उसपर दूसरी या तीसरी मंज़िल बन सकती है। गोया किसी ग़लत आभास या किसी ग़लत तरीक़े से अगर कोई स्वीकृति प्राप्त की गई हो तो वह स्वीकृति जायज़ नहीं होगी। इसके और उदाहरण भी मैं अभी दूँगा। इसका उद्देश्य यह है कि हर वह स्वीकृति जो किसी ग़लत तरीक़े से या ग़लत-बयानी से जिसको ‘तदलीस’ भी कहा जाता है, प्राप्त की गई हो, जिसका स्पष्टीकरण हदीसों में मौजूद है, वह स्वीकृति अस्वीकार्य है और इसके परिणामस्वरूप जो ‘बैअ’ (सौदा) की जाएगी वह फ़ासिद (अवैध) होगी। और ‘मुतज़र्रर’ व्यक्ति, यानी जिस पक्ष को नुक़्सान हुआ है, उसको यह अधिकार है कि वह चाहे तो इस ‘बैअ’ को निरस्त कर दे।
सबके लिए समान क़ानून
दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त जो शरीअत ने दिया है वह यह है कि मामलात यानी व्यवहार का क़ानून राज्य के तमाम नागरिकों के लिए समान होगा। इसमें मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम, भले और बुरे, शिक्षित और अशिक्षित का कोई भेदभाव नहीं होगा। मदीना मुनव्वरा के नागरिक राज्य में जिस क़ानून का पालन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) स्वयं पर करते थे, उसी क़ानून का पालन एक यहूदी पर भी अनिवार्य होता था। इसी एक क़ानून का पालन यसरिब (मदीना) के ग़ैर-मुस्लिम बहुदेववादियों पर भी अनिवार्य होता था। और दूसरे ग़ैर-मुस्लिमों पर भी होता था। इसलिए व्यवहार और व्यापार का क़ानून सबके लिए बराबर है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने उसूल बयान किया है कि “मामलात यानी लेन-देन और व्यापार यानी सिविल लॉ में ज़िम्मी यानी वह ग़ैर-मुस्लिम नागरिक जिसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी इस्लामी राज्य ने ली हो, उसकी हैसियत बिलकुल मुसलमानों जैसी है।” जो चीज़ मुसलमानों के लिए नाजायज़ है वह इस ज़िम्मी के लिए भी नाजायज़ है और जो चीज़ मुसलमानों के लिए जायज़ है वह इस ज़िम्मी के लिए भी जायज़ है, कुछ अपवादों के साथ। इन अपवादों में ग़ैर-मुस्लिमों को मुसलमानों के मुक़ाबले में ज़्यादा छूट दी गई हैं। मैंने ‘माले-मुतक़व्विम’ से सम्बन्धित चर्चा में बताया था कि अगर किसी ग़ैर-मुस्लिम के पास शराब हो और कोई मुसलमान उसको नष्ट कर दे तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी मुसलमान के पास शराब हो और ग़ैर-मुस्लिम उसको नष्ट कर दे तो उसको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसलिए कि मुसलमान किसी नाजायज़ और हराम चीज़ का मालिक नहीं हो सकता और ग़ैर-मुस्लिम हो सकता है।
इन अपवादों के अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था को संगठित करनेवाला सारा क़ानून मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों के लिए समान है। इसमें न धर्म की क़ैद है, न मिल्लत की क़ैद है, न इलाक़े की क़ैद है और न कोई और बंदिश है। यह दूसरा सिद्धान्त है जो शरीअत ने दिया है।
ज़ुल्म को समाप्त करना
तीसरा सिद्धान्त है ‘रफ़अ-ज़ुल्म’ यानी ज़ुल्म को समाप्त करना कि किसी भी व्यापारिक लेन-देन में किसी पक्ष पर ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से तो इससे सब धर्म और क़ानून सहमत हैं। आप दुनिया के किसी भी धर्म के अनुयायियों से पूछें कि तुम ज़ुल्म को जायज़ समझते हो? हर धर्म जवाब में यही कहेगा कि नहीं हम ज़ुल्म को जायज़ नहीं समझते। लेकिन इस दावे के बावजूद व्यावहारिक जगत् के दूसरे धर्मों, देशों और व्यवस्थाओं में ऐसे क़ानून प्रचलित हैं जिनको शरीअत ज़ुल्म समझती है और जायज़ नहीं समझती। उसकी वजह यह है कि बहुत-सी चीज़ों में ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी का प्रभाव ज़ाहिर और स्पष्ट नहीं होता, बल्कि छिपा रहता है और जब तक गहराई से ग़ौर न किया जाए उसका आभास नहीं होता। शरीअत ने अपने आदेशों और निर्देशों के द्वारा छिपे हुए ज़ुल्म के यह अदृश्य रास्ते बंद कर दिए हैं। उदाहरण के रूप में अगर दो आदमियों में व्यापार हो रहा है। उदाहरणार्थ आपसे मैंने यह गिलास ख़रीदा। अब मैं इसका मालिक हो गया। और इसकी क़ीमत पचास रुपये मुझे अदा करनी है। आपका हक़ यह है कि आपको ये पचास रुपय मिल जाएँ। मेरा हक़ यह है कि यह गिलास मुझे मिल जाए। लेकिन अगर कोई शर्त ऐसी रख ली गई हो कि जिसमें किसी एक पक्ष का हित एक तरफ़ा तौर पर प्रभावित होता हो वह ‘बैअ’ जायज़ नहीं है। उदाहरणार्थ आप यह कहें कि मैंने यह गिलास बेच तो दिया, लेकिन प्रयुक्त करने का अधिकार मुझे होगा, तुम्हें नहीं होगा। ज़ाहिर है कि यह ‘बैअ’ नहीं है और न शरीअत में ऐसा मामला जायज़ है। शरीअत की नज़र में यह ज़ुल्म है कि आपने क़ीमत तो वुसूल कर ली और पैसे ले लिए, लेकिन जब मेरे इस्तेमाल की बारी आई तो आपने यह शर्त रख दी कि इसके इस्तेमाल का हक़ आपको है। अत: कोई ऐसी शर्त जिसमें किसी एक पक्ष को ऐसा कोई फ़ायदा या advantage निश्चित तौर पर दिया गया हो, किसी ऐसे ऐडवांटेज़ की गारंटी दी गई हो जो आम तौर पर व्यापारियों के रिवाज के अनुसार इस पक्ष को नहीं मिलना चाहिए और वह अपने लिए गारंटी करना चाहे तो ऐसा क्रय-विक्रय जायज़ नहीं होगा। यह ‘तराज़ी’ के ख़िलाफ़ है और ज़ुल्म है।
पूर्ण न्याय
जब यह स्वीकार कर लिया जाए कि दोनों पक्षों के अधिकार उनको पूर्ण रूप से मिलने चाहिएँ। जिस व्यापार और कारोबार का जो उद्देश्य बाज़ार में बैठनेवालों के सामने है वह उद्देश्य दोनों पक्षों के लिए समान रूप से पूरे हों, तो फिर चौथा उसूल हमारे सामने आता है कि पूरा अद्ल और मुकम्मल क़िस्त होना चाहिए। क़ानूनी इंसाफ़ भी हो और वास्तविक इंसाफ़ भी हो। मैं बता चुका हूँ कि अद्ल का अर्थ क़ानूनी इंसाफ़ और क़िस्त के अर्थ वास्तविक न्याय है। क़ानूनी इंसाफ़ से मुराद यह है कि लेन-देन की दस्तावेज़ात, विवरण और गवाह, ये सब-के-सब चरण और अपेक्षाएँ पूर्ण रूप से क़ानून के अनुसार और अद्ल की अपेक्षाओं के अनुसार पूरी हों। पवित्र क़ुरआन की सूरा-2 बक़रा की आयते-मदाइना (आयत-282) में इसका विवरण बयान किया गया है कि व्यापार और लेन-देन के आदेश क्या हैं। सूरा-2 बक़रा की कई आयतों में यह विवरण बयान हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारियाँ उस समय तक समाप्त नहीं होतीं जब तक वे वास्तविक इंसाफ़ की अपेक्षाओं का ध्यान न रखें। अगर मुझे यह मालूम है कि मैं इस गिलास का मालिक नहीं हूँ और मैं इसको जेब में डालकर ले जाऊँ और जाकर बेच दूँ, तो क्रय-विक्रय के बारे में क़ानून की हद तक क़ानून के ज़ाहिरी तक़ाज़े पूरे हो गए। मैंने गिलास दे दिया, दस्तावेज़ भी लिख दी, क़ीमत भी मार्केट के अनुसार है, रसीद भी दे दी। अब अगर वह व्यक्ति अदालत में जाएगा तो मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकेगा। अदालत यह देख लेगी कि मैंने गिलास का क़ब्ज़ा उसको दे दिया। दस्तावेज़ में लिखी हुई रक़म के अनुसार भुगतान किया है, वुसूल करने की रसीद भी ले ली है। तो ये तमाम क़ानूनी तक़ाज़े पूरे हो गए हैं। लेकिन यह मूल वास्तविकता न अदालत को मालूम है और न उस पक्ष को मालूम है कि यह गिलास मेरे पास कहाँ से आया। यह बात उनमें से किसी के ज्ञान में नहीं कि यह गिलास मैं यहाँ से छिपाकर जेब में रखकर ले गया था। इसलिए वास्तविक इंसाफ़ का, जो मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है, तक़ाज़ा यह है कि मैं उसकी क़ीमत वापस कर दूँ और उससे कहूँ कि मुझे यह गिलास अस्ल मालिक को वापस करना है। आप चाहें तो मैं इस जैसा एक और गिलास आपको दे सकता हूँ। या वास्तविक मालिक से पूछ लूँ कि वह बेचने के लिए राज़ी है तो क़ीमत देकर गिलास आपको दे दूँ। जब मैं ये सारे काम करवा लूँगा तो यह वास्तविक इंसाफ़ होगा और क़ानूनी इंसाफ़ भी पूरा हो जाएगा। यह अन्तर है क़ानूनी और वास्तविक इंसाफ़ में, जिनका ध्यान रखना दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारी है और उनको ध्यान रखना चाहिए।
सद्दे-ज़रिया (रास्ता रोकना)
पाँचवाँ उसूल जो पवित्र क़ुरआन ने बयान किया है और जिसपर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बड़े विस्तृत आदेश संकलित किए हैं वह ‘सद्दे-ज़रिया’ है। ‘ज़रिया’ का अर्थ vehicle या रास्ता, या means और ‘सद्दे-ज़रिया’ का अर्थ है रास्ते को बंद करना। किसी ज़रिये का रोकना। पवित्र क़ुरआन ने यह सिद्धान्त दिया है कि अगर कोई चीज़ अपने-आपमें जायज़ हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कोई बुराई पैदा हो रही हो तो फिर वह जायज़ चीज़ नाजायज़ क़रार पाएगी। इसके उदाहरण पवित्र क़ुरआन और हदीसों दोनों में आए हैं। पवित्र क़ुरआन में है कि “अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं, तुम उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग न करो। ऐसा न हो कि वे हद से आगे बढ़कर अज्ञानवश अल्लाह के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगें।” (क़ुरआन, 6:108) इसलिए कि अगर तुम उनको बुरा कहोगे तो वे अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बुरा कहेंगे। गोया तुम्हारा उनको बुरा कहना अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को बुरा कहने का ज़रिया बनेगा। अत: तुम उनके लात और मनात को भी बुरा न कहो। लात और मनात और दूसरे बुतों को बुरा कहने का निषेध इसलिए है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताख़ी करनेवाले गुस्ताख़ी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें कोई ऐसा काम जो चाहे अपने-आपमें बुरा न हो, नहीं करना चाहिए ताकि इसके परिणामस्वरूप वह बुराई पैदा न हो जिसको शरीअत भी बुराई स्वीकार करती है और स्वाभाविक रूप से भी जिसे बुराई स्वीकार किया जाता है। इससे यह नियम निकला कि सद्दे-ज़रिया के नियम के तहत बहुत-से जायज़ कामों से भी बचना चाहिए और यह कि सद्दे-ज़रिया के नियम के तहत कभी-कभी जायज़ कामों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। दूसरा उदाहरण फ़त्हे-मक्का के बाद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया कि अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि तुम्हारी क़ौम इस्लाम के बारे में बद-गुमानी का शिकार हो जाएगी तो मैं काबा का दोबारा इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के आधार पर निर्माण करता। जब हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने काबा बनाया था तो चतुर्भुज रूप में बनाया था। यह एक चतुर्भुज इमारत थी और एक तरफ़ से इस की शक्ल अंडाकार थी। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के ज़माने से बैतुल्लाह इसी तरह चला आ रहा था। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) किशोरावस्था में थे तो मक्का मुकर्रमा में बाढ़ आई। इस बाढ़ से जहाँ और बहुत-सा नुक़्सान हुआ, वहाँ बैतुल्लाह की इमारत भी गिर गई। आप में से जिन लोगों को मक्का मुकर्रमा जाने का मौक़ा मिला है, उन्होंने देखा होगा कि बैतुल्लाह इस तरह से एक घाटी के बिल्कुल बीच में स्थित है जिस तरह से एक बहुत बड़ा कटोरा होता है और उसके बीच में उभरी हुई जगह बनाते हैं इस तरह से बैतुल्लाह बना हुआ है। जब भी बारिश होती थी तो सारा पानी बैतुल्लाह के प्रांगण में जमा हो जाता था। अब भी हो जाता है। चुनाँचे बारिश हुई। सैलाब आया और बैतुल्लाह की इमारत गिर गई। क़ुरैश के अधर्मियों ने यह तय किया कि हम बैतुल्लाह की इमारत दोबारा बनाएँगे और बिलकुल जायज़, पाकीज़ा और हलाल आमदनी से इसको बनाएँगे। नवनिर्माण के इस काम में किसी भी प्रकार की नाजायज़ या ज़ुल्म की आमदनी शामिल नहीं होगी। उनकी आमदनी में ‘रिबा’, ब्याज और डाका और अन्य कई तरह की नाजायज़ आमदनियाँ शामिल होती थीं। वह भी उनको नाजायज़ आय समझते थे। उनके ज़ेहन में भी वे आय सही नहीं थीं, लेकिन शैतान के बहकाने से वे आमदनियाँ उनके पास आ रही थीं। बैतुल्लाह के बारे में उन्होंने तय किया कि हर दृष्टि से पाकीज़ा और साफ़ आमदनी को इस्तेमाल किया जाएगा। अत: जिनके पास ऐसी आमदनी थी कि जिसके बारे में उसको विश्वास था कि यह पाकीज़ा और सुथरी आमदनी है उसने लाकर जमा करा दी। क़ुरैश के इस्लाम विरोधियों ने इस तरह से बैतुल्लाह के नवनिर्माण का काम शुरू कर दिया कि बैतुल्लाह की दरवाज़ेवाली दिशा से काम का आरम्भ हुआ। हज्रे-असवद वाली दिशा पूर्ण हो गई। शेष तीनों आयामों की दीवारें उठ गईं। रुक्ने-इराक़ी और रुक्ने-शामी के दरमियानवाली दीवार का हिस्सा रह गया। जब वे यहाँ तक पहुँचे तो पैसे समाप्त हो गए। जब संसाधन समाप्त हो गए तो उन्होंने तय किया कि जहाँ तक काम हो गया है वहाँ एक दीवार बनाकर फ़िलहाल बैतुल्लाह की इमारत को बंद कर दिया जाए और शेष हिस्से में एक छोटी-सी दीवार निशानी के लिए बना दी जाए। जब जायज़ आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो इसको हम दोबारा बना देंगे। चुनाँचे इतना ही हिस्सा बनाकर छोड़ दिया। इसपर कई वर्ष गुज़र गए। सम्भवत: पंद्रह-बीस वर्ष गुज़र गए। इसी दौरान में सर्वोच्च अल्लाह ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को नबी बनाया और उन्होंने ने नुबूवत का एलान किया तो सबका ध्यान इस एलान की तरफ़ हो गया। और न केवल मक्का, बल्कि पूरा प्रायद्वीप अरब दो प्रतिद्वंद्वी कैम्पों में विभाजित हो गया। बहुत-से लोग इस्लाम के विरोधी हो गए। और कुछ इस्लाम दुश्मनी में यह बात भूल गए कि बैतुल्लाह का निर्माण भी पूरा करना है। जब मक्का मुकर्रमा फ़त्ह हुआ तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से फ़रमाया कि अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि तुम्हारी क़ौम इस्लाम के बारे में बद-गुमान हो जाएगी तो मैं बैतुल्लाह की इमारत को गिराकर दोबारा हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियादों पर क़ायम करता और अस्ल नक़्शे के अनुसार उसको बहाल कर देता। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह ख़तरा था कि अगर बैतुल्लाह की इमारत को दोबारा बनाने के लिए गिराया गया तो जिन लोगों के दिल में ईमान पक्का नहीं है, या जो वैसे ही इस्लाम के दुश्मन हैं या मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) हैं तो वे यह कहेंगे कि अब तक तो मिल्लते-इबराहीमी (इबराहीम का समुदाय) की पैरवी का दावा हो रहा था, बैतुल्लाह को केन्द्र बनाया जा रहा था और जब सफलता प्राप्त हुई तो पहला काम यह किया कि इबराहीमी केन्द्र को ही गिरा दिया। इसके परिणामस्वरूप जो लोग मक्का में नहीं हैं और जो अरब क़बीले बाहर फैले हुए हैं, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था या इस्लाम उनमें फैल रहा था, उनमें बद-गुमानी पैदा होगी और ख़तरा है कि बहुत-से लोग इस्लाम से फिर जाएँगे। लोगों का इस्लाम से फिर जाना और गुमराही में मुब्तला हो जाना एक बहुत बड़ी बुराई है। इसके मुक़ाबले में अगर बैतुल्लाह किसी और नक़्शे पर क़ायम है तो यह इससे कमतर दर्जे की बुराई है। बैतुल्लाह के नक़्शे में कसर रह जाने के बावजूद सच यह है कि नमाज़ें हो रही हैं, हज भी हो रहा है, उमरा भी हो रहा है, तवाफ़ भी हो रहा है और बैतुल्लाह क़िबला का काम भी दे रहा है, सब काम हो रहे हैं और लोग बजाय एक पूरी दीवार के एक छोटी और अधूरी दीवार के गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं। जब हाजी तवाफ़ करते हैं तो हतीम की बाहरी दीवार के बाहर से तवाफ़ करते हैं। इसका एक आंशिक लाभ यह हुआ कि आम आदमी जिसको बैतुल्लाह में प्रवेश का मौक़ा नहीं मिलता वह ‘हतीम’ में जाकर नमाज़ पढ़ लेता है, वह भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। हज़ारों लाखों इंसानों को रोज़ मौक़ा मिलता है और वे ‘हतीम’ में नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे शायद मौक़ा न मिलता। तो यह एक छोटे-से दर्जे की बुराई, जो पता नहीं कि अब इन परिस्थितियों में बुराई है भी कि नहीं, और अगर है भी तो बहुत मामूली दर्जे की है, इसकी वजह से इतना बड़ा नुक़्सान उठाया जाए कि लाखों आदमियों के ईमान को ख़तरे में डाल दिया जाए और ऐसे ख़तरे में डाल दिया जाए कि वे इस्लाम से ही फिर जाएँ, यह बहुत बड़ी बुराई है, इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इससे गुरेज़ किया।
इन दो उदाहरणों से अनुमान होगा कि सद्दे-ज़रिया शरीअत में एक मौलिक सिद्धान्त की हैसियत रखता है। ऐसा मौलिक सिद्धान्त जिसकी रौशनी में बहुत-से आदेश दिए गए और बहुत-से क़ानून दिए गए। उनमें से कुछ का विस्तृत विवरण मैं अभी बयान करता हूँ। इन क़ानूनों की तत्वदर्शिता और निहितार्थ सद्दे-ज़रिया है।
दौलत का समाज में घूमते रहना
छटा मौलिक सिद्धान्त जो पवित्र क़ुरआन ने दिया है वह यह है कि इस्लाम धन-दौलत को समाज के शरीर के लिए ख़ून की तरह ज़रूरी समझता है। जैसे मेरे और आपके शरीर के लिए ख़ून की गति ज़रूरी और अपरिहार्य है इसी तरह से समाज के शरीर के लिए धन-दौलत का घूमते रहना अपरिहार्य है। अगर किसी इंसान के शरीर से पूरा ख़ून निचोड़ लिया जाए तो वह मर जाएगा। इसी तरह अगर किसी समाज या राज्य से उसकी पूरी दौलत खींच ली जाए, तो राज्य भी शेष नहीं रह सकेगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने धन को ‘क़ियामन लिन्नास’ कहा है, कि माल वह चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को स्थायित्व प्राप्त होता है, जिसके आधार पर समाज ज़िन्दा रहता है। फिर जिस तरह से ख़ून एक व्यक्ति की जीवन में महत्व रखता है इसी तरह से समाज की जीवन में भी धन महत्व रखता है। एक व्यक्ति के शरीर के हर हिस्से में ख़ून होना चाहिए। उंगली में भी ख़ून होना चाहिए, टाँग में भी होना चाहिए और सिर में भी होना चाहिए। जिस हिस्से में ख़ून नहीं होगा वह हिस्सा निष्क्रय हो जाएगा। किसी के हाथ में ख़ून न आए तो हाथ निष्क्रय हो जाएगा और काम नहीं करेगा। जब ख़ून ख़राब होता है तो शरीर बीमार हो जाता है और जब ख़ून साफ़ होता है तो शरीर स्वस्थ होता है। शरीर के जिस हिस्से को ख़ून की जितनी आवश्यकता है उतना ख़ून मिलता रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। आवश्यकता से कम मिले तो शरीर बीमार होता है। यही हाल समाज के शरीर का है। धन-दौलत को शरीर के हर हिस्से में समान रूप से पहुँचना चाहिए। जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ख़ून वहाँ जाना चाहिए, ताकि शरीर का कोई हिस्सा जीवन के इस ज़रिये से वंचित न हो। यह पवित्र क़ुरआन की नज़र में माल या धन की धारणा है। इसी लिए पवित्र क़ुरआन ने कहा कि “ताकि वह (माल) तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न लगाता रहे।” (क़ुरआन, 59:7) इस सिद्धान्त के तहत बहुत-से आदेश दिए गए हैं। कुछ आदेश हदीसों में दिए गए हैं और कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने तर्कों से मालूम किए हैं।
उदाहरण के रूप में शरीअत यह कहती है कि हर व्यक्ति को अपने तौर पर माल में ‘तसर्रुफ़’ (उपभोग) का अधिकार है। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप अपने माल में किस तरह ‘तसर्रुफ़’ करें। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने माल का ऐसा उपभोग करने लगे कि इससे दौलत का संकेन्द्रण होने लगे और दौलत का फैलाव रुक जाए तो फिर यह पवित्र क़ुरआन के इस मौलिक आदेश के ख़िलाफ़ होगा। अत: राज्य की ज़िम्मेदारी होगी कि वहाँ हस्तक्षेप करे और इस संकेन्द्रण को रोक दे। उदाहरणार्थ अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत दी है। आप यह करें कि बाज़ार में जितने डॉलर हैं सब ख़रीद लें। प्रतिदिन खरब-दो-खरब रुपये के डॉलर आप ख़रीद लिया करें। तो परिणाम यह निकलेगा कि बाज़ार में शायद डॉलर का अभाव पैदा हो जाएगा और जो डॉलर आज 58 रुपये का है वह शायद सौ, एक सौ अट्ठावन रुपये का हो जाए। डॉलर की क़ीमत बढ़ जाने से पाकिस्तानी रुपये की क़ीमत गिर जाएगी। इसलिए राज्य की ज़िम्मेदारी है कि आपको ऐसा न करने दे। आप अगर कहें कि मुझे शरीअत ने अपने माल में ‘तसर्रुफ़’ (उपभोग) का अधिकार दिया है, अत: मैं जो चाहूँ खरीदूँ और जो चाहूँ बेचूँ। जो डॉलर बेच रहा है वह भी अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है वह भी अपनी स्वतंत्र मर्ज़ी से ख़रीद रहा है। लेकिन इस ‘तराज़ी’ (आपसी सहमति) के बावजूद इस तरह के लेन-देन की अनुमति नहीं है। इसलिए कि पवित्र क़ुरआन ने दौलत के दौलतमंदों के एक सीमित वर्ग के दरमियान संकेन्द्रण को नाजायज़ क़रार दिया है। धन का यह संकेन्द्रण अद्ल और ज़ुल्म के उन्मूलन की इस्लामी धारणा के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर आप यह चाहें कि बाज़ार में जितना गेहूँ है, सब ख़रीदकर अपने गोदामों में भर लें और कहें कि ऐसा करने का मुझे शरीअत के अनुसार अधिकार है। शरीअत ने मुझे यह हक़ दिया है कि मैं जिस तरह से चाहूँ अपनी दौलत का उपभोग करूँ। उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार यह तार्किकता भी अस्वीकार्य है और ऐसे कारोबार की अनुमति नहीं है जो धन के संकेन्द्रण को जन्म दे। जब एक व्यक्ति के पास गेहूँ का अधिकतर भाग जमा हो जाएगा तो शेष व्यापारी कहाँ से बेचेंगे। और जब व्यापारियों के पास बेचने के लिए गेहूँ नहीं होगा, तो गेहूँ का अभाव पैदा हो जाएगा। यों उसकी क़ीमत बढ़ जाएगी। माँग और पूर्ति की demand और supply की व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। इसलिए इस स्वाभाविक व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत इसमें हस्तक्षेप करे। इसपर आप ग़ौर करते जाएँ तो बहुत-से आदेशों का कारण और तत्वदर्शिता मालूम हो जाएगी। वे आदेश भी जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यापार और मालियात से है और वे आदेश भी जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यापार और मालियात से नहीं है। लेकिन वे परोक्ष रूप से देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में विरासत का क़ानून। शरीअत ने विरासत का क़ानून जिन बहुत-सी तत्वदर्शिताओं की वजह से दिया है उनमें से एक तत्वदर्शिता यह भी है कि धन-दौलत एक जगह संकेन्द्रित न हो। एक व्यक्ति ने जायज़ तरीक़े से धन-दौलत को प्राप्त किया। उसके मरने के बाद उसका माल उसके आठ दस अन्य वारिसों में वितरित हो जाएगा। फिर इन वारिसों की और तीन चार नस्लों में वितरित हो जाएगा। इस तरह से एक परिवार की दौलत बीस परिवारों में वितरित हो जाएगी।
शरीअत के आदेशों के विभिन्न विभागों का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र का शादी-ब्याह से सम्बन्ध लोगों को नज़र नहीं आता। इस्लाम की नज़र में सम्बन्ध है। इस्लाम का स्वभाव यह है कि लोग दूर-दूर के परिवारों में शादियाँ करें। क़रीबी परिवारों में शादियाँ कम करें। क़रीबी परिवारों में शादियाँ हराम नहीं, मकरूह भी नहीं, लेकिन इस्लाम ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके कारण तो बहुत-से हो सकते हैं, मेडिकल भी और सामाजिक भी। लेकिन एक कारण यह भी है कि जब एक परिवार की दौलत वितरित होगी तो उसका कुछ हिस्सा ऐसे परिवारों को भी पहुँचेगा जो पहले से रिश्तेदार नहीं थे और सम्भव है कि तुलनात्मक रूप से ग़रीब भी थे। जब उनके यहाँ वह हिस्सा और ज़्यादा वितरित होगा तो किसी और परिवार में भी चला जाएगा। यों दौलत फैलती जाएगी।
इस तरह ज़कात के आदेश हैं, उनके भी बहुत-से उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दौलत के संकेन्द्रण को तोड़ना है। अव्वल तो शरीअत ने नसीहत यह की है कि जो दौलत आवश्यकता से अधिक है वह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दो। आईडियल बात तो यही है कि जो कुछ आवश्यकता से अधिक है वह सब कुछ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने ऊँचे स्तर पर न जा सके, तो उसके लिए आदेश यह है कि जितना ख़र्च कर सकता हो वह ख़र्च करो। ख़र्च करने के बाद जो बच जाए वह बचाने की अनुमति है, लेकिन बचत करके उसको बेकार छोड़ देने की अनुमति नहीं है। इसकी नसीहत नहीं की गई, नसीहत यह की गई है कि इसको व्यापार में लगाया जाए, ताकि व्यापार में लगने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और दौलत बेकार न पड़ी रहे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कई हदीसों में इसकी नसीहत की गई कि दौलत को घर में जमा न रखो, बल्कि व्यापार और कारोबार में लगाओ। जब व्यापार और कारोबार में लगाओगे तो आर्थिक गतिविधि फैलेगी और इससे दौलत में फैलाव भी पैदा होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लोगों के व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा।
मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति दौलत को व्यापार में नहीं लगाता और घर में ही बचाकर रखता है। और ये सारे रास्ते और छेद जिनके ज़रिये दौलत छन-छनकर जमा होती हो, जो शरीअत ने बंद कर दिए हैं इसके बावजूद उसके पास कुछ दौलत जमा हो जाए तो हर वर्ष उसकी ढाई प्रतिशत ज़कात देनी पड़ेगी। एक व्यक्ति आख़िर कितने वर्ष ज़िन्दा रहेगा? पाँच दस साल, बीस साल, पचास साल? आख़िरकार उसकी जमा की हुई दौलत वारिसों के पास पहुँचेगी तो वे भी ढाई प्रतिशत वार्षिक ज़कात देंगे। यों एक-आध नस्ल के बाद दौलत के संकेन्द्रण की सारी सम्भावनाएँ समाप्त हो जाएँगी। इस्लाम ने किसी रेडिकल या ऐसे फ़ैसले का आदेश नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप समाज में कोई हलचल और अफ़रातफ़री पैदा हो जाए। पिछली सदी में लोगों ने देखा कि कुछ के पास दौलत का संकेन्द्रण है। उन्होंने आव देखा न ताव और सब कुछ नेशनलाइज़ करने के नाम पर क़ौमी मिल्कियत में ले लिया और वह सारी दौलत, सारे कारख़ाने, हर चीज़ तबाह हो गई और आज तक तबाह चली आ रही है। पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों में वह अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी। इस्लाम ने ऐसी अनुचित और अव्यावहारिक शिक्षा नहीं दी। इस्लाम का स्वभाव हर चीज़ में क्रमशः और स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ने का है। जो काम नेशनलाइज़ेशन करनेवाले एक दिन में करना चाहते थे और सत्तर-अस्सी वर्षों में भी नहीं कर सके। अगर इस्लाम के आदेशों पर अमल करते तो पच्चीस-तीस वर्षों में इन उद्देश्यों पर कार्यान्वयन हो जाता। इस कार्य-पद्धति पर चलने में न प्रतिक्रिया पैदा होती, न किसी के दिल में डर पैदा होता, न किसी का नुक़्सान होता, बल्कि इससे भाई-चारा और नैतिक आचरण और आध्यात्मिकता का माहौल अलग पैदा होता, वह एक अतिरिक्त फ़ायदा होता। पवित्र क़ुरआन ने एक सार्वजनिक आयत में धोखे से मना किया है। एक-दूसरे को धोखा मत दो। एक-दूसरे का माल ग़लत तरीक़े से मत खाओ। ग़लत तरीक़े से खाने की एक शक्ल यह भी है कि एक व्यक्ति का हित तो सुरक्षित हो और दूसरे का हित सुरक्षित न हो। यह चीज़ शरीअत के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। इसलिए शरीअत ने बहुत-से आदेश ऐसे दिए हैं जिसका उद्देश्य इस रास्ते को बंद करना है। अगर हित है तो दोनों को सम्मान क़रीब-क़रीब मिलना चाहिए। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उसकी मेहनत का उतना फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अगर कोई ख़तरा और रिस्क है तो दोनों उसमें बराबर के हिस्सेदार हों। यह अद्ल और इंसाफ़ और शरीअत दोनों की अपेक्षा है। ये वे मौलिक सिद्धान्त हैं जो पवित्र क़ुरआन ने बयान किए हैं और जिनका विवरण अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान किया है।
शरीअत की सीमाओं के अन्दर व्यापार की हर शक्ल जायज़ है
व्यापार की जितनी शक्लें इंसान सोच सकता है वे सब जायज़ हैं। मैंने पहले बताया है कि मामलात में शरीअत का स्वभाव बहुत नर्मी का है। कुछ चीज़ें जो नाजायज़ थीं, वे शरीअत ने रोक दीं। कुछ चीज़ें जो करने की थीं वे शरीअत ने कह दिया कि यह अनिवार्य करनी हैं। इन दोनों के दरमियान कारोबार और व्यापार की जो-जो सम्भावित सूरतें हैं वे सब जायज़ हैं, बशर्तेकि उसके परिणामस्वरूप कोई और ख़राबी पैदा न हो। यह आप सद्दे-ज़रिया से देख लें।
व्यापार की जितनी शक्लें हो सकती हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। कारोबार की कुछ शक्लें तो वे हैं जिनमें माल के बदले माल हो। आपने पैसे देकर किताब ले ली। एक तरफ़ किताब है और दूसरी तरफ़ पैसे हैं। एक तरफ़ भी माल है, दूसरी तरफ़ भी माल है। आपने गाँव में बाग़ किसी को दे दिया और शहर में मकान ख़रीद लिया। यह भी माल के बदले माल है। जितनी भी किस्में हैं वे क्रय-विक्रय हो या बार्टर सेल हो। ये तमाम वे क़िस्में हैं जिनमें माल के बदले माल है। यह वह मामला है जिसको शरीअत की शब्दावली में ‘बैअ’ कहते हैं। सर्वोच्च अल्लाह ने ‘बैअ’ यानी व्यापार को जायज़ और ‘रिबा’ को हराम क़रार दिया है। व्यापार और कारोबार की दूसरी क़िस्में वे हैं जिनमें आधार ज़मीन या ज़मीन की पैदावार हो। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति ज़मीन उपलब्ध करेगा, दूसरा उसपर मेहनत करेगा। या उदाहरणार्थ एक व्यक्ति बीज देगा, दूसरा शेष मेहनत करेगा। एक बीज भी उपलब्ध करेगा और मेहनत भी करेगा और दूसरा व्यक्ति केवल ज़मीन देगा। यों इस प्रबन्ध की बहुत-सारी शक्लें हो सकती हैं जिनके विवरण में जाने का मौक़ा नहीं। फिर यह कारोबार अब केवल खेती के साथ ही जुड़ा नहीं रहा। अब ज़मीन से सम्बन्धित कारोबार में खनिज पदार्थ, तेल की तलाश और ऐसे ही बहुत-से मामलात भी शामिल हो गए हैं जिनके लिए नए-नए आदेश निकालने की आवश्यकता है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने आम तौर से खेती ही के सन्दर्भ में चर्चा की है। उनकी चर्चा आम तौर पर दो शीर्षकों के तहत होती है। एक ‘मुज़ारअत’ और दूसरा ‘मुसाक़ात’। ‘मज़ारअत’ से मुराद साझा कारोबार का वह अंदाज़ है जिसको बटाई भी कह सकते हैं। इसकी कुछ शक्लें जायज़ और कुछ नाजायज़ हैं। जो नाजायज़ हैं वे इसलिए नाजायज़ हैं कि उनमें या तो ‘रिबा’ पाया जाता है या उस तरह की कोई और चीज़, जिसको मैं आगे स्पष्ट कर रहा हूँ।
‘मुज़ारअत’ की कुछ शक्लें वे भी हैं जो उन सिद्धान्तों से टकराती हैं जिनका अभी मैंने उल्लेख किया। अलबत्ता ‘मुज़ारअत’ की हर वह शक्ल जो सिद्धान्तों से टकराती नहीं है और इसमें हुर्मत (निषेध) का कोई और पहलू नहीं पाया जाता वह जायज़ है। व्यापार और कारोबार की कुछ क़िस्में वे हैं जिनमें एक तरफ़ मेहनत होती है और दूसरी तरफ़ पैसा होता है। मेहनत हर तरह की हो सकती है। शारीरिक मेहनत भी हो सकती है और मानसिक मेहनत भी हो सकती है। आप अकाउंटेंट हैं। हिसाब-किताब में लोगों को मश्वरे देते हैं और इसकी फ़ीस लेते हैं। आप ऑडिटर हैं या वकील हैं और अपनी दक्षता से लोगों को उचित मश्वरा देते हैं, यह भी मानसिक मेहनत की एक शक्ल है कि आप मश्वरा देकर फ़ीस लेते हैं। एक व्यक्ति मज़दूर है और ईंटें उठाकर तीसरी मंज़िल पर ले जाता है। यह भी मेहनत की एक शक्ल है। गोया मेहनत अपनी तमाम शक्लों के साथ एक तरफ़ हो और मुआवज़ा दूसरी तरफ़ हो तो यह वह चीज़ है जिसको ‘मुज़ारबा’, ‘मुशारका’ या ‘इजारा’ कहा जाता है।
कारोबार की चौथी क़िस्म वह है कि जिसमें वास्तविक आधार संगठन यानी organization पर हो। दो पक्ष मिलकर किसी कारोबार को संगठित करें। दोनों पक्ष संगठन में साझेदार हों। यह ‘मुशारका’ की अधिकतर क़िस्में हैं। ‘मुशारका’ की बहुत सारी क़िस्में और बहुत-सा विस्तृत विवरण है।
धन का वितरण
आगे बढ़ने से पहले धन के वितरण के बारे में एक मौलिक चीज़ बताना चाहता हूँ। शरीअत ने बहुत-से ऐसे आदेश दिए हैं जिनका अर्थव्यवस्था और व्यापार से तो कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा यह भी होता है कि दौलत के संकेन्द्रण से नजात मिलती है और दौलत धीरे-धीरे फैलती चली जाती है। इन अप्रत्यक्ष रूप से किए गए कामों के साथ-साथ शरीअत ने कुछ आदेश ऐसे भी दिए हैं जिनका प्रत्यक्ष उद्देश्य यही मालूम होता है कि दौलत के संकेन्द्रण को रोका जाए। उनमें से एक हिस्सा वाजिब और अनिवार्य है। दूसरा हिस्सा मात्र पसंदीदा है, जिसकी नसीहत की गई है, लेकिन उसको अनिवार्य क़रार नहीं दिया गया है।
शरीअत के इन आदेशों में जो हिस्सा अनिवार्य और पालन योग्य है उसमें सबसे पहले नफ़क़े (गुज़ारा ख़र्च) के आदेश हैं। कुछ लोगों का नफ़क़ा और अन्य ख़र्चे शरीअत के अनुसार आपके ज़िम्मे वाजिब हैं। उदाहरणार्थ पत्नी का नफ़क़ा पति के ज़िम्मे है। सन्तान का नफ़क़ा बाप के ज़िम्मे है। बूढ़ी माँ जिसका कोई सहारा नहीं, उसका नफ़क़ा जवान बेटों पर है। बूढ़ा बाप जिसकी अपनी आमदनी नहीं है उसका नफ़क़ा उसके बेटों के ज़िम्मे है। विधवा बहन जिसकी कोई आमदनी नहीं उसका नफ़क़ा भाई के ज़िम्मे है। पवित्र क़ुरआन ने नफ़क़ा-ए-वाजिबा (भरण-पोषण का अनिवार्य ख़र्च) के सिलसिले में एक सार्वजनिक सिद्धान्त दे दिया है कि ‘वारिस के ज़िम्मे भी वैसा ही है’। इसका अर्थ यह है कि हर वह व्यक्ति जिसके आप किसी-न-किसी हवाले से वारिस हो सकते थे, अगर वह ज़रूरतमन्द हो और आपके पास संसाधन हों तो उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ पड़ती है। यह नफ़क़ा-ए-वाजिबा है, जिसका विवरण फ़ुक़हा ने संकलित किया है। पवित्र क़ुरआन ही से ये तमाम आदेश निकलते हैं।
दूसरा वाजिब या फ़र्ज़ विभाग इस मामले में विरासत के आदेश का है। विरासत के आदेशों के तहत एक व्यक्ति की दो तिहाई दौलत अनिवार्य रूप से उसके मरने के बाद वितरित हो जाएगी। विरासत के शरई आदेशों के महत्व को दुनिया ने अभी तक नहीं समझा। दुनिया अभी तक यह समझती है कि धन-दौलत का एक जगह संकेन्द्रित होना अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। जब कि पवित्र क़ुरआन उसको अलाभकारी समझता है। इंग्लैंड में आज 2004 में भी primogeniture का सिद्धान्त प्रचलित है। इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि विरासत पर सबसे बड़े बेटे का हक़ हो। वहाँ सम्पत्ति की मालियत अगर एक ख़ास हद से अधिक हो तो उसका कोई और रिश्तेदार या व्यक्ति परिवार वारिस नहीं हो सकता सिवाय सबसे बड़े बेटे के। इस सिद्धान्त के तहत सबसे बड़ा बेटा ही सारी सम्पत्ति का वारिस होता है और शेष सब वारिस वंचित रहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इंग्लैंड के इस उसूल पर कोई आपत्ति नहीं करता। औरतों के अधिकारों के ध्वजावाहक भी ख़ामोश हैं। कम-से-कम मैंने किसी पश्चिमी या पूर्वी महिला के बारे में कभी यह नहीं सुना जिसने इसपर आपत्ति की हो कि यह इंसाफ़ के ख़िलाफ़ और औरतों के साथ ज़्यादती है। मुझे नहीं मालूम कि शरई आदेशों के ख़िलाफ़ और महिलाओं के स्वरचित अधिकारों के पक्ष में प्रतिदिन प्रदर्शन करनेवाली महिलाएँ इसपर क्यों चुप रहती हैं। यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है। बड़ी-बड़ी जायदादों और जागीरों में सारी-की-सारी पैतृक सम्पत्ति केवल बड़े बेटे को मिलेगी, लेकिन इसमें से न पत्नी को कुछ मिलेगा, न बहनों को मिलेगा, न बेटियों को मिलेगा और न माँ को कुछ मिलेगा, बल्कि सब कुछ बड़े बेटे को मिलेगा। कोई नहीं पूछता कि छोटे बेटे को क्यों नहीं मिलेगा? बहनों को क्यों नहीं मिलेगा? यह एक अजीब-सी बात है। अगर बेटा न हो। भाई, बाप और चचा भी न हो, चचेरा भाई या उसका बेटा भी न हो तो फिर नवासे को मिलेगा। बेटियों को फिर भी नहीं मिलेगा। अब सिवाय इसके कि यह एक सरासर धाँधली और ज़ुल्म है इसके सिवा कोई और वजह मालूम नहीं होती। शरीअत ने ऐसा कोई अत्याचारपूर्ण आदेश नहीं रखा। विरासत के आदेशों का पालन अनिवार्य है और मरनेवाले की मौत के तुरन्त बाद ही उसके छोड़े हुए धन और सम्पति को वितरित किया जाएगा। “इसके पश्चात् कि जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए, या जो ऋण हो उसे चुका दिया जाए।” (क़ुरआन, 4:12) इसके बाद वसीयत पर कार्यान्वयन किया जाएगा और इसके बाद जो बचेगा वह वारिसों में हिस्से के तौर पर वितरित कर दिया जाएगा।
तीसरी चीज़ ज़कात है जो हर व्यक्ति को देनी है। ज़कात ढाई प्रतिशत से लेकर बीस प्रतिशत तक है। जहाँ बीस प्रतिशत है इसको ‘ख़ुमुस’ कहते हैं। कुछ जगह दस प्रतिशत है जिसको ‘उश्र’ कहते हैं। कुछ जगह पाँच प्रतिशत है जिसको ‘निस्फ़ुल-उश्र’ कहते हैं। और शेष जगह ढाई प्रतिशत है। शरीअत ने बहुत-से मामलात में शरीअत के आदेशों के उल्लंघन पर आर्थिक कफ़्फ़ारात (प्रायश्चित) भी रखे हैं। अतीत में दुनिया की कोई व्यवस्था इस्लाम के सिवा ऐसी नहीं थी और आज भी नहीं है जिसने दौलत के संकेन्द्रण को तोड़ने के लिए विशुद्ध आध्यात्मिक मामलों और धार्मिक आदेशों को प्रयुक्त किया हो। जिसने विशुद्ध धार्मिक प्रकार के आदेशों में ग़रीबों और दरिद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध किया हो। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का रोज़ा टूट जाए या कोई जान-बूझकर रोज़ा तोड़ दे तो वह क्या करेगा। साठ मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। इस तरह उसका कफ़्फ़ारा अदा हो जाएगा जो विशुद्ध धार्मिक चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ़ दौलत भी वितरित होगी। साठ मिस्कीनों तक वह दौलत पहुँचेगी, हालाँकि यह एक विशुद्ध धार्मिक ग़लती है। एक विशुद्ध आध्यात्मिक और व्यक्तिगत मामला है जिस तरह कि दुनिया की नज़र में धार्मिक मामले व्यक्तिगत होते हैं। लेकिन यहाँ इस विशुद्ध व्यक्तिगत और आध्यात्मिक मामले को मिस्कीनों तक दौलत और संसाधन पहुँचाने का ज़रिया बना दिया गया। कल मैं क़त्ले-शुब्हे-अमद और क़त्ले-ख़ता के सिलसिले में यह कहना भूल गया था कि क़त्ले-ख़ता और क़त्ले-शुब्हे-अमद में कफ़्फ़ारा अदा करने का भी आदेश है। कफ़्फ़ारा अनिवार्य रूप से अदा किया जाएगा जिसका विवरण सूरा-4 निसा में मौजूद है। अब जब कफ़्फ़ारा अदा किया जाएगा तो ग़लती से होनेवाले क़त्ल के रूप में कफ़्फ़ारे के तौर पर ग़रीबों जो कुछ दिया जाएगा, उसके परिणामस्वरूप दौलत का एक और हिस्सा फैलेगा। इसलिए कफ़्फ़ारा के सारे आदेश देख लें। उनमें धन के वितरण का प्रबन्ध हर स्थिति में नज़र आएगा। झूठी क़सम खा ली तो दस मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अमुक काम हो गया तो इतने मिस्कीनों को खाना खिलाओ। हज में ग़लती हो गई तो दुंबा ज़ब्ह करके ग़रीबों में वितरित करो। बड़ी ग़लती हो जाए तो ऊँट या गाय ज़ब्ह करके बाँटो या उसके पैसे ग़रीबों को दे दो। यह एक ऐसी चीज़ है जिसपर ग़ौर करें तो बहुत-सी तत्वदर्शिताएँ आपके सामने आएँगी कि शरीअत ने किस तरह अपने अंगों को एक-दूसरे से सम्बद्ध किया है। ख़ालिस इबादतें आर्थिक मामलों से जुड़ी हैं। उनके आर्थिक परिणाम निकल रहे हैं। विशुद्ध आर्थिक मामलों के लाभ आध्यात्मिक जीवन में सामने आ रहे हैं। पैसा ख़र्च किया, लेकिन नमाज़, या हज या रोज़े में जो ग़लती हो गई थी उसकी भरपाई हो गई।
कल मैंने ‘ज़मान’ और ‘दियत’ का ज़िक्र किया था। क़त्ले-शुब्हे-अमद और क़त्ले-ख़ता में ‘दियत’ दी जाती है। ‘दियत’ की रक़म अगर सोने के अनुसार हो और आजकल के हिसाब से मान लीजिए कि दस लाख रुपय हों तो अनुमान करें कि कितनी रक़म दी जाएगी। हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) का कथन है “इस्लाम में कोई ख़ून बेकार नहीं जा सकता।” अगर क़ातिल पकड़ा गया है तो उससे क़िसास लिया जाएगा। शुब्हे-अमद या ख़ता है तो उससे ‘दियत’ ली जाएगी। क़ातिल का पता नहीं चलता लेकिन यह अनुमान है कि इस इलाक़े के लोगों में से कोई है तो ‘क़सामत’ और ‘दियत’ होगी। और अगर उनमें से कोई स्थिति मौजूद या सम्भव नहीं है तो राज्य उसका ज़िम्मेदार होगा।
इसी तरह से ‘अर्श’ का आदेश है। यह भी एक शब्दावली है जिसपर कल समय मिला तो कुछ और बात होगी। ज़ख़्म की ‘दियत’ को ‘अर्श’ कहते हैं। ‘शज्जह’ में कितनी ‘दियत’ होगी। ‘शज्जह’ की कौन-सी क़िस्मों में कितनी ‘दियत’ है। इसको ‘अर्श’ कहते हैं। ये वे चीज़ें हैं जो अनिवार्य हैसियत रखती हैं। इन्ही में से एक चीज़ वह है जिसको फ़िक़्ह की शब्दावली में ‘नवाज़िल’ कहते हैं। ‘नवाज़िल’ से मुराद वह एमरजेंसी टैक्स है जो राज्य को किसी हंगामी स्थिति में लगाने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ जंग हो गई और जंग के ख़र्चों से मुक्त होने के लिए राज्य को नया टैक्स लगाना पड़ा। सैलाब आ गया, जैसा कि सन् 1970 में जब पूर्वी पाकिस्तान में सैलाब आया था, तो जनरल यह्या की हुकूमत ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हर गैलन पेट्रौल पर एक रुपये की वृद्धि की थी जो आज तक हम अदा कर रहे हैं। इसमें कितना बंगालियों को मिला और कितना नहीं मिला, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन पिछले 34 वर्षों से हम वह हंगामी टैक्स चुका रहे हैं और अब भी यह सिलसिला जारी है। जब आप पेट्रौल ख़रीदते हैं या गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आपको वह टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इस तरह के टैक्सों का तो मैं नहीं कह सकता कि वे ‘नवाज़िल’ के दायरे में आते हैं या मात्र जग्गा टैक्स की हैसियत रखते हैं। लेकिन जहाँ वाक़ई एमरजेंसी हो और हुकूमत को टैक्स लगाना पड़े तो शरीअत के आदेश के अनुसार वह टैक्स लगा सकती है और जनसाधारण के लिए वह टैक्स अदा करना अनिवार्य होगा। इस तरह कुछ और ख़र्चे हैं जो मंदूब यानी मुस्तहब (पसंदीदा) हैं। इसके परिणामस्वरूप भी दौलत वितरित होगी। सदक़ा-ए-नाफ़िला है। पवित्र क़ुरआन और हदीसों में सदक़े का आदेश जगह-जगह दिया गया है। हर मुसलमान के बारे में आईडियल बात यह है कि अपने पास ग़ैर-ज़रूरी दौलत जमा न करे और सदक़ा कर दे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक रात भी ऐसी नहीं गुज़ारी कि आपके पास धन-दौलत का कोई हिस्सा मौजूद हो। एक बार मस्जिद में बैठे थे और सम्भवत: रात वहाँ इबादत में गुज़ारने का इरादा था। अचानक कोई चीज़ याद आ गई तो परेशान होकर घर पहुँच गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो किसी ने पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! यह क्या बात थी?” फ़रमाया कि “दो दीनार घर में रह गए थे और मुझे याद नहीं रहा था कि वह घर में पड़े रह गए हैं, और मुझे अल्लाह के सामने बहुत शर्मिन्दगी होती अगर मैं ऐसे हाल में रात गुज़ारता कि मेरे घर में दो दीनार रखे हों। इसलिए मैंने जाकर उनको सदक़ा कर दिया।”
अस्ल आईडियल तो यह है। अगर कोई इंसान इस आईडियल तक पहुँच सकता है तो बहुत बड़ी बात है। पहुँचनेवाले इस दर्जे तक पहुँचते भी हैं। लेकिन अगर कोई इस आईडियल तक न पहुँच सके तो जितना उसके क़रीब हो सके, उतना उसको क़रीब होने की कोशिश करनी चाहिए और जितना अल्लाह के रास्ते में सदक़ा कर सके वह करना चाहिए। उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि दौलत वितरित होगी।
‘बदले-सुलह’, यह भी एक शब्दावली है। इससे अभिप्रेत है कि किसी ऐसे मुक़द्दमे में किसी ऐसे मामले में जिसमें इंसानों का हक़ हावी हो, दोनों पक्ष आपस में राज़ीनामा कर लें और एक पक्ष दूसरे को इस राज़ीनामे के बदले में कुछ देने को तैयार हो जाए तो यह जायज़ है। शरीअत ने इसकी अनुमति दी है। ‘बदले-सुलह’ पैसे के रूप में भी हो सकता है। सम्पत्ति के रूप में भी हो सकता है। चल-सम्पत्ति भी हो सकती है और अचल-सम्पत्ति भी हो सकती है। लेकिन यह चूँकि वाजिब या अनिवार्य नहीं है इसलिए इसको ‘वाजिबात’ में नहीं रखा बल्कि ‘मुस्तहबात’ में रखा है। सुलह (सन्धि) करना चूँकि शरीअत में मुस्तहब है और सुलह का आधार अगर किसी मुआवज़े पर हो तो वह भी जायज़ है, बल्कि बेहतर है। बेहतरीन तो यह है कि बिना पैसे के सुलह की जाए, लेकिन अगर उसके लिए कोई तैयार न हो तो फिर थोड़ा-सा मुआवज़ा लेकर समझौता किया जा सकता है। शरीअत ने इसकी अनुमति दी है।
मुहर्रमाते-तिजारत (निषिद्ध व्यापार)
ये तो वे मौलिक सिद्धान्त हैं जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नत में बयान हुए हैं। जिनकी पैरवी अवश्य ही करनी चाहिए। यह वे उसूल हैं जो हर कारोबार, हर व्यापार और हर लेन-देन में मौजूद होने चाहिएँ। अगर उनका उल्लंघन होगा तो कारोबार या लेन-देन जायज़ नहीं होगा। इनके अलावा पंद्रह चीज़ें वे हैं जो ‘मुहर्रमात’ हैं, यानी वे चीज़ें जो शरीअत ने हराम क़रार दी हैं। इन पंद्रह में से कोई एक चीज़ भी अगर किसी कारोबार में पाई जाएगी तो वह कारोबार नाजायज़ होगा। इन पंद्रह ‘मुहर्रमात’ से बचते हुए और उन मौलिक सिद्धान्तों पर अमल करते हुए जो अभी मैंने बयान किए, जो भी कारोबार किया जाएगा वह जायज़ होगा। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए जो भी कारोबार किया जाएगा वह इस्लामी कारोबार होगा। इसके बारे में शब्दावलियों के मामले में कोई विवाद नहीं। इस कारोबार का जो जी चाहे नाम रख लें, उसके लिए जो चाहें तरीक़ा अपना लें। इसके जो चाहें विवरण तय कर लें, शरीअत ने इन बातों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा।
1. ‘रिबा’
इन मुहर्रमात में सबसे बड़ा तत्व ‘रिबा’ है। ‘रिबा’ यानी ब्याज को शरीअत ने पूरी तरह हराम क़रार दिया है और मुसलमानों से यह कहा है कि जितने भी ब्याज आधारित कर्ज़े या माँगें हैं उनको फ़ौरी तौर पर समाप्त कर दो। जो अस्ल रक़म है वह वुसूल करो, न कम न ज़्यादा। न स्वयं ज़ुल्म उठाओ और न दूसरे पर ज़ुल्म करो। और अगर कोई व्यक्ति इससे बाज़ न आए तो “फिर अल्लाह और रसूल की तरफ़ से उसके ख़िलाफ़ एलाने-जंग है।” (क़ुरआन, 2:279) यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक ईसाई क़बीले के साथ अनुबन्ध किया। नजरान दक्षिणी अरब में यमन के क़रीब एक इलाक़ा था, वहाँ ईसाइयों के कुछ क़बीले रहते थे। क़बीले का नाम नजरान नहीं था, इलाक़े का नाम नजरान था। इन ईसाइयों से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो अनुबन्ध किया उसके तहत उन ईसाइयों को वहाँ रहने के अधिकार दिए गए। उनको नागरिकता की तमाम रिआयतों से नवाज़ा गया। उनको तमाम धार्मिक रस्में करने की अनुमति दी गई और ये सारे अधिकार इस अनुबन्ध में लिखे गए। इसके साथ-साथ उसमें यह भी लिखा गया कि तुम ‘रिबा’ का कारोबार नहीं करोगे। अगर तुममें से किसी ने ‘रिबा’ का कारोबार किया तो फिर यह अनुबन्ध निरस्त समझा जाएगा। यह सख़्त शब्द इसमें आए हैं। ‘रिबा’ किसे कहते हैं। ‘रिबा’ हर ऐसी बढ़ोतरी को कहते हैं जो किसी देय रक़म में की जाए और किसी एक पक्ष की तरफ़ से दूसरे पक्ष से अनिवार्य रूप से वुसूल की जाए, वह बढ़ोतरी जिसके मुक़ाबले में न कोई अतिरिक्त सौदा हो, न कोई मेहनत हो, न कोई रिस्क हो और न कोई सेवा हो। सेवा, मेहनत, मुआवज़ा या रिस्क या ज़मान, इन चारों की अनुपस्थिति में मात्र समय के मुक़ाबले में अगर कोई वृद्धि वुसूल की जाएगी वह ‘रिबा’ कहलाएगी। यह चीज़ शरीअत के बहुत-से आदेशों से टकराती है और पवित्र क़ुरआन के मौलिक और पूरी तरह निषिद्ध मामलों में से है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ब्याज की बुराई को बयान करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं कि उनको सुनकर रौंगटे खड़े हो जाते हैं।
2. ‘ग़रर’
दूसरी चीज़ है ‘ग़रर’ से बचना। ‘ग़रर’ के शाब्दिक अर्थ हैं किसी कारोबार में किसी एक पक्ष के हित का किसी ऐसी स्थिति से शर्त से जुड़ा होना जो उसके अधिकार में न हो। गोया ऐसी अनिश्चितता जिससे किसी एक पक्ष का अधिकार निश्चित रूप से अनिर्धारित और सन्दिग्ध क़रार पा जाए। अभी मैं उदाहरण देता हूँ। आपने किसी व्यक्ति से मामला किया कि मैं रावल डैम में शिकार खेलने जा रहा हूँ। आप मुझे एक हज़ार रुपये दे दीजिए और जितनी मछलियाँ मिलेंगी वे सब आपकी होंगी। यह मामला ‘ग़रर’ कहलाता है और शरीअत के अनुसार नाजायज़ है। इसलिए कि यहाँ एक पक्ष का हक़ यानी एक हज़ार रुपये तो क़तई और निश्चित रूप से निर्धारित है, जबकि दूसरे पक्ष का अधिकार बिलकुल अस्पष्ट, सन्दिग्ध और वश से बाहर है। हो सकता है कि शिकार के परिणामस्वरूप एक किलो मछली हाथ आ जाए, हो सकता है एक भी न आए। हो सकता है दस किलो मछली आ जाए। अब उनमें से एक पक्ष का हित तो तय है और उसको एक हज़ार रुपये मिल गए। दूसरे का हित निर्धारित नहीं है कि एक मछली मिलेगी या दस मिलेंगी। जो दस मिलेंगी वे दस-दस किलो की होंगी कि पचास-पचास किलो की होंगी। यह ‘ग़रर’ कहलाता है और नाजायज़ है।
इस तरह के कारोबार की जितनी भी शक्लें हैं उन सबसे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मना किया है और उनमें से एक-एक की मनाही हदीस में आई है। इसके उदाहरण हदीसों में बहुत हैं। उदाहरणार्थ आप कहें कि आप इतनी रक़म दें और मैं आपके लिए यह परिंदा जो आसमान में उड़ रहा है आपको दे दूँगा। हो सकता है कि वह परिंदा आपके हाथ ही न लगे। यह भी सम्भव है कि आप उसका शिकार करने के लिए गोली चलाएँ और इसके बजाय कोई दूसरा परिंदा चपेट में आ जाए। ये सारी चीज़ें ‘ग़रर’ हैं और इसके आधार पर कोई कारोबार जायज़ नहीं है।
इंशोरेंस के बहुत-से प्रकारों में ‘ग़रर’ होता है इसलिए वे प्रकार नाजायज़ होंगे। आपने प्रीमियम चुका दिया। यह तो सबको मालूम है कि आपने क्या चुकाया। लेकिन आपको क्या मिलेगा यह निश्चितता के साथ किसी को मालूम नहीं। सम्भव है बहुत कुछ मिले और यह भी सम्भव है कि कुछ भी न मिले। लाइफ़ इंशोरेंस के कुछ प्रकारों में कहा जाता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे घरवालों को इतने पैसे मिलेंगे और अगर न मरा तो कुछ नहीं मिलेगा। यह जायज़ नहीं है। या अगर मर गया तो ज़्यादा मिलेगा और अगर न मरा तो कम मिलेगा। अब मरना न मरना तो मेरे अधिकार में नहीं है इसलिए उसके आधार पर मेरे हक़ में कमी-बेशी ‘ग़रर’ कहलाएगी। इसलिए ऐसी सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं जिनमें ‘ग़रर’ का तत्व शामिल हो।
3. ‘क़िमार’
तीसरी चीज़ है ‘क़िमार’, जिसको जुआ कहते हैं। कोई ऐसा कारोबार जिसमें एक आदमी का लाभ हो और साथ ही दूसरे आदमी का निश्चित रूप से नुक़्सान हो रहा हो, ‘क़िमार’ कहलाता है। उदाहरणार्थ दस आदमियों ने सौ-सौ रुपये जमा किए और लॉटरी से वह सारी रक़म एक को मिल गई। नौ आदमियों के सौ-सौ रुपये बरबाद हो गए और एक आदमी को बहुत कुछ मिला। जिस आदमी को बहुत कुछ मिला वह मात्र भाग्य और संयोग से मिला। इस कारोबार में मेहनत या दक्षता का कोई अमल-दख़ल नहीं। जो वंचित हुए वे मात्र भाग्य एवं संयोग से वंचित हुए। यह ‘क़िमार’ कहलाता है और शरीअत में हराम है। इंशोरेंस की कुछ शक्लों में भी ‘क़िमार’ पाया जाता है।
4. ‘मैसिर’
चौथी चीज़ ‘मैसिर’ है। यह भी ‘क़िमार’ ही की एक शक्ल है। इसमें किसी एक पक्ष का नुक़्सान होना तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो फ़ायदा किसी एक व्यक्ति को होता है वह किसी एक पक्ष को बिना किसी हक़ और अधिकार के प्राप्त होता है। जबकि इसमें सबने समान रूप से हिस्सा लिया था। यह बड़ी बारीक चीज़ है। उदाहरण के रूप में कुछ कंपनियाँ यह करती हैं कि आप हमसे टूथपेस्ट खरीदें। इसमें एक कार्ड निकलेगा और इसपर एक नम्बर लिखा होगा। अगर आपका नम्बर निकल आया तो आपको गाड़ी मिलेगी या इतना नक़द इनाम मिलेगा। यह ‘मैसिर’ है। इसलिए कि टूथपेस्ट तो सबने समान रूप से ख़रीदा था। और यह कंपनी गाड़ी या नक़द रक़म मुफ़्त तो नहीं देती। अगर बाज़ार में टूथपेस्ट की क़ीमत दस रुपये है तो यह कंपनी साढ़े दस रुपये की देती है। इस तरह से अतिरिक्त आमदनी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा वे इनाम में ख़र्च करते हैं। इसमें ‘रिबा’ भी है, ‘क़िमार’ भी है, ‘मैसिर’ भी है और यह ज़ुल्म है। फ़र्ज़ कीजिए आप कहें कि नहीं जी, इनामवाले टूथपेस्ट और दूसरे टूथ पेस्टों की क़ीमत में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन अगर शेष टूथ पेस्टों को ख़रीदने के लिए दस आदमी प्रतिदिन आते हैं तो इसको ख़रीदने के लिए सौ आदमी आते हैं। सेल बढ़ जाती है। उसने धोखे से बिक्री बढ़ा दी और इसके परिणामस्वरूप उसको जो फ़ायदा हुआ, उसको दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय एक थोड़ा हिस्सा लोगों को इनाम के तौर पर दे दिया और शेष लोगों को वंचित कर दिया। तो यह शरीअत के स्वभाव और अद्ल और इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है और ‘मैसिर’ कहलाता है। ‘मैसिर’ भी नाजायज़ है, लेकिन ‘क़िमार’ उसकी सबसे बुरी शक्ल है और बड़े दर्जे का हराम है।
5. ‘जह्ल’
पाँचवीं चीज़ जहालत और जानकारी न होना है। कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना या बेचना, जिसका प्रकार आपको मालूम नहीं है। वह जायज़ नहीं है। एक व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे एक लाख रुपय दे दें मैं यहाँ के लिए आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ डेस्क बनाकर दे दूँगा। यह कारोबार दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि नहीं मालूम कि वह जो डेस्क लाकर देगा वह किस तरह का होगा। लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा। अच्छी लकड़ी का होगा या बुरी लकड़ी का। ऊपर कोई रेक्सीन लगा होगा या नहीं लगा होगा। जब तक निर्धारित रूप से यह पहले ही तय न कर लिया जाए कि वह किस शक्ल, किस डिज़ाइन, किस प्रकार और किस चीज़ से बना होगा उस समय तक उसका क्रय-विक्रय जायज़ नहीं है। यह ‘जह्ल’ है जिसमें किसी एक पक्ष का हित अस्पष्ट हो और अज्ञात हो।
6. ‘ग़बने-फ़ाहिश’
छटी चीज़ ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है। ‘ग़बने-फ़ाहिश’ फ़ुक़हा की एक शब्दावली है। अरबी शब्दावली में ग़बन का अर्थ धोखाधड़ी होता है। लेकिन पारिभाषिक अर्थ की दृष्टि से हर धोखे को ग़बन नहीं कहते। इससे मुराद धोखे का एक विशेष प्रकार है। यानी यह ग़बन उर्दू वाला ग़बन नहीं है। उर्दू में embezzelment को ग़बन कहते हैं। फ़िक़्ह की शब्दावली में ‘ग़बने-फ़ाहिश’ से मुराद है किसी ख़रीदार के अनजानेपन या परेशानी से फ़ायदा उठाते हुए किसी कारोबार या किसी चीज़ का इतना लाभ लेना जो बाज़ार को देखते हुए बहुत ज़्यादा हो। यानी exhorbitant profiteering, इसको ‘ग़बने-फ़ाहिश’ कहते हैं और यह जायज़ नहीं है।
‘ग़बने-फ़ाहिश’ का अपराध आम तौर से दो स्थितियों में होता है। या तो दूसरा पक्ष मजबूर होता है। और उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर बहुत ज़्यादा लाभ वुसूल कर लिया जाता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी सख़्त परेशानी या जल्दबाज़ी की वजह से बाज़ार के भाव मालूम करने का मौक़ा नहीं मिलता। अभी मैंने इसका उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति मजबूर है, उसका कोई क़रीबी अज़ीज़ किसी बीमारी में मुब्तला है और इलाज पर में लाख रुपये ख़र्च होंगे। वह अपना तीस लाख रुपये की मालियत का मकान आपको बीस लाख रुपये में देने के लिए तैयार हो जाए। यह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है। बाज़ार में इस मकान की क़ीमत अगर तीस लाख नहीं होगी तो अट्ठाईस लाख तो ज़रूर होगी। तीस नहीं तो उनत्तीस ज़रूर होगी। मार्केट के मूल्य से मामूली कमी-बेशी की तो गुंजाइश है। लेकिन इस मामूली कमी-बेशी के मुक़ाबले में जितना आप ज़्यादा लेंगे तो वह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ माना जाएगा। और यह असाधारण लाभ कमानेवाले के लिए नाजायज़ है। दूसरी सूरत यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के न जानने की वजह से ‘ग़बने-फ़ाहिश’ का जुर्म करता है। उदाहरणार्थ इस्लामाबाद में एक आदमी बाहर से आया। उसे मकानों की क़ीमत का कोई पता नहीं। आप दो करोड़ का मकान उसको पाँच करोड़ में बेच दें तो यह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ होगा।
इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने भलीभाँति स्पष्ट रूप से ग़बन की परिभाषा करने की कोशिश की है। हनफ़ी फ़ुक़हा की रायों का संक्षिप्तीकरण ‘मुजल्ला अल-अहकामुल-अदलिया’ की सम्बन्धित धाराओं में मौजूद है। हनफ़ी फ़ुक़हा ने ग़बन की दो क़िस्में बयान की हैं।
- ‘ग़बने-यसीर’ यानी मामूली ग़बन
- ‘ग़बने-फ़ाहिश’ यानी गम्भीर प्रकार का ग़बन
इन दोनों क़िस्मों के अलग-अलग आदेश बयान किए गए हैं। ग़बने-फ़ाहिश ‘मुजल्ला अल-अहकामुल-अदलिया’ की धारा 165 के अनुसार वह है जिसमें उक्त उप वस्तुओं का बाज़ार भाव आम भाव से—
- आम साज़ो-सामान में पाँच प्रतिशत से अधिक
- जानवरों में दस प्रतिशत से अधिक
- अचल-सम्पत्ति सम्पत्ति में बीस प्रतिशत से अधिक
लगाया गया हो। इससे कम लाभ लिया गया हो तो वह ‘ग़बने-यसीर’ है। ‘ग़बने-फ़ाहिश’ के साथ अगर ‘‘तग़रीर’’ भी हो तो बात और भी serious हो जाती है। इस स्थिति में ख़रीदार को ‘बैअ’ निरस्त करने का हक़ (ख़ियारे-ग़बन) प्राप्त होता है। लेकिन यह बात उल्लेखनीय है कि यतीम के वक़्फ़ माल और बैतुलमाल का मुतवल्ली (प्रबन्धक) अगर ‘ग़बने-फ़ाहिश’ का शिकार हो तो चाहे ‘‘तग़रीर’’ हो या न हो ‘बैअ’ बातिल और निरस्त होगी।
7. ‘ज़रर’
व्यापार में निषिद्ध चीज़ों में सातवीं चीज़ ‘ज़रर’ है। कोई भी ऐसा कारोबार या व्यापार जिसमें किसी को ऐसा नुक़्सान पहुँचा हो जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं पहुँचता, वह ‘ज़रर’ कहलाता है। हदीस में आया है कि “न नुक़्सान उठाओ न जवाबी नुक़्सान पहुँचाओ।” ‘ज़रर’ के आधार पर शरीअत में बहुत विस्तृत आदेश दिए गए हैं और इस विषय पर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने दर्जनों किताबें लिखी हैं कि ‘ज़रर’ के आदेश क्या हैं। इस समय किसी विस्तृत चर्चा की तो गुंजाइश नहीं, कि समय बहुत तंग हो रहा है। फ़िलहाल ये तीन चार जुमले काफ़ी हैं कि ‘ज़रर’ से मुराद वह नुक़्सान है जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम के परिणामस्वरूप उठाने पर मजबूर हो जिसका उठाना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। न जिसको उठाने में उसपर कोई ज़िम्मेदारी है, न उसकी किसी ढिलाई को अमल-दख़ल है, वह ‘ज़रर’ है। शरीअत का आदेश यह है कि न आप ‘ज़रर’ उठाएँ और न किसी ‘ज़रर’ के जवाब में दूसरे को ‘ज़रर’ पहुँचाएँ। जवाबी ‘ज़रर’ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी व्यक्ति ने आपके मकान की दीवार गिरा दी। यह उसने आपको ‘ज़रर’ पहुँचाया। अब आपके लिए जायज़ नहीं कि वहाँ जाकर उससे बदला लें और उसके मकान की दीवार गिरा दें। यहाँ क़िसास नहीं चलता। आपको जो मुआवज़ा मिलेगा वह यह कि आप दीवार को दोबारा बनाने का ख़र्चा गिरानेवाले से वुसूल कर लें। इससे ज़्यादा कुछ माँग करने का आपको कोई हक़ प्राप्त नहीं और विशेषकर उसकी दीवार गिराने की अनुमति तो बिलकुल नहीं है। किसी ने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो जवाब में आपके लिए जायज़ नहीं कि आप भी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दें। इस उसूल के तहत आपका हक़ है कि आप अपने टूटे हुए शीशे की क़ीमत वुसूल कर लें।
8. परस्पर टकराते कारोबार
आठवीं चीज़, जिससे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मना किया है। वह दो परस्पर टकराते कारोबारों को इकट्ठा करना है। हदीस के अनुसार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इससे मना किया है कि दो अलग-अलग और विभिन्न कारोबारों को इस तरह आपस में मिला दिया जाए कि दोनों के हित एक-दूसरे के अधीन हो जाएँ, एक-दूसरे पर निर्भर हो जाएँ। यह जायज़ नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक आम क्रय-विक्रय है। यह जायज़ है, लेकिन मैं यह कहूँ कि यह क़लम आप मुझे एक लाख रुपये में बेच दें और इसके बदले मैं आपको एक हज़ार रुपये क़र्ज़ दे दूँगा। यह जायज़ नहीं होगा। ये दोनों मामले एक-दूसरे के साथ inconsistant हैं। अव्वल तो इस क़लम का बाज़ार भाव एक लाख रुपये नहीं है। फिर यह एक हज़ार रुपये जो आप शर्त करके मुझसे ले रहे हैं। यह इससे inconsistant है और इस तरह के मिश्रित मामलों से ‘रिबा’ का रास्ता खुलता है। कुछ कारोबार ऐसे हैं कि अगर इन दो कारोबारों को आपस में मिला दिया जाए तो उसके परिणामस्वरूप या ‘रिबा’ क़ायम होगा यह ‘क़िमार’ होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दो inconsistant और परस्पर असम्बद्ध कारोबारों को एक-दूसरे पर निर्भर dependable बनाने की और एक-दूसरे पर दारोमदार करने की मनाही की है। दो अलग-अलग कारोबार हों तो हो सकते हैं। अगर दोनों कारोबार अपनी-अपनी जगह जायज़ हैं। आप दोनों करें, यह ठीक है। लेकिन एक कारोबार का हित दूसरे पर निर्भर हो और दूसरे का हित पहले पर निर्भर हो यह दुरुस्त नहीं है।
9. ‘बैए-मादूम’
नौवीं चीज़ जिसकी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मनाही की, वह ‘बैए-मादूम’ है। हदीस में कहा गया है, “जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वह मत बेचो।” अत: जो चीज़ आपकी मिल्कियत और क़ब्ज़े में नहीं है उसकी बिक्री जायज़ नहीं है। आजकल फ़्यूचर सेल्ज़ का कारोबार बड़े ज़ोर-शोर से होता है। शेयर्ज़ का कारोबार भी आम तौर से फ़्यूचर सेल के आधार पर होता है और फ़्यूचर सेल्ज़ का आधार ‘बैए-मादूम’ पर होता है। इसमें सारा कारोबार क़र्ज़ के आधार पर होता है। न ख़रीदनेवाले को ख़रीदी हुई चीज़ का क़ब्ज़ा मिलता है और न बेचनेवाले के क़ब्ज़े में वह चीज़ होती है। मात्र काग़ज़ी और फ़र्ज़ी कार्रवाइयों के आधार पर यह कारोबार होते-होते कहीं-से-कहीं पहुँच जाता है। उदाहरणार्थ अमुक कंपनी जो आगे चलकर स्टाक मार्केट में लॉन्च होगी, उसके एक लाख शेयर्ज़ किसी ने ख़रीद लिए हैं। अभी न कंपनी लॉन्च हुई है न उसकी चीज़ें लॉन्च हुई हैं और आपने उसके एक लाख शेयर्ज़ ख़रीद लिए। जब कंपनी लॉन्च करने का समय आया तो देखनेवालों ने देखा कि पार्टी बड़ी मज़बूत है, उसके पास पैसे और संसाधन बहुत हैं। ख़याल है कि इस कंपनी के शेयर्ज़ की क़ीमत और भी बढ़ेगी। आपने पहले ही उसके शेयर को बेचना और ख़रीदना शुरू कर दिया। अभी न कंपनी अस्तित्व में आई है न माल है और न कोई और चीज़ फ़िलहाल मौजूद है। और एक लाख का शेयर आपने पाँच लाख रुपये में बेच दिया। जब कंपनी लॉन्च हुई तो मालूम हुआ कि उसको किसी बड़े बैंक ने अंडर राइट कर दिया था और दस रुपये वाला शेयर पचास रुपये का हो गया और किसी और ने ख़रीद लिया। यह जो ख़रीद-दर-ख़रीद है यह इस तरह होती है कि न कोई चीज़ आपके क़ब्ज़े में है न आपकी मिल्कियत में है। यह सारा कारोबार मात्र काग़ज़ी और काल्पनिक है। यह जायज़ नहीं है। यह भी ‘रिबा’ और ‘क़िमार’ का रास्ता खोलता है। अत: शरीअत ने ऐसे कारोबार की मनाही की है और कहा है कि जो चीज़ तुम्हारी मिल्कियत में नहीं, उसकी बिक्री भी जायज़ नहीं है। इसमें ‘बैए-सलिम’ और ‘अक़्दे-इस्तिंसा’ का अपवाद है।
10. ‘तग़रीर’
दसवीं चीज़ जिसकी मनाही है वह धोखा है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसके लिए ‘तग़रीर’ की शब्दावली प्रयुक्त की है। ‘तग़रीर’ से मुराद यह है कि ख़रीदार के सामने माल की ऐसी परिभाषा और description की जाए जो उसमें मौजूद न हो। ‘मुजल्ला अल-अहकामुल-अदलिया’ की धारा 164 की व्याख्या करते हुए मुजल्ला के टीकाकारों ने ‘तग़रीर’ का उदाहरण देते हुए लिखा है कि बाए (बेचनेवाला) अगर यह दावा करे कि उसके माल या चीज़ की मालियत इतनी है और वह चीज़ दर-हक़ीक़त उतनी मालियत की न हो तो यह भी ‘तग़रीर’ है।
कुछ फ़ुक़हा ने ‘तग़रीर’ की दो क़िस्में क़रार दी हैं—
1. तग़रीरे-क़ौली (अपनी बात से धोखा देना)
2. तग़रीरे-फ़ेली (अपने कृत्य से धोखा देना)
दोनों के अलग-अलग आदेश और परिणामों पर हनफ़ी फ़ुक़हा ने विस्तृत बहस की है। इन आदेशों का सारांश ‘मुजल्ला अल-अहकामुल-अदलिया’ के व्याख्याताओं विशेषकर अल्लामा अली हैदर और अल्लामा ख़ालिद उनासी ने अपनी-अपनी टीकाओं में दिया है।
11. ‘तसर्रुफ़’ फ़ी मुल्किल-ग़ैर (दूसरे देश में उपभोग)
ग्यारवीं चीज़ जिसकी मनाही है वह दूसरे की मिल्कियत में ‘तसर्रुफ़’ है। आप जिस चीज़ का कारोबार कर सकते हैं, या जिस सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का आपको अधिकार है, उसके लिए ज़रूर है कि वह बेचनेवाले की पूर्ण मिल्कियत में हो। अधूरी और अपूर्ण मिल्कियत में ज़मान यानी risk कभी अधूरा और त्रुटिपूर्ण और कुछ स्थितियों में सिरे से होता ही नहीं है। शरीअत का नियम है कि जिस चीज़ का ज़मान आपके ज़िम्मे न हो उसका लाभ वुसूल करना आपके लिए जायज़ नहीं है। हदीस में आया है कि “अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उस चीज़ का लाभ लेने से मना किया है जिसका ज़मान (risk) आपके ज़िम्मे न हो।”
12. ‘एहतिकार’
बारहवीं चीज़ जिसकी मनाही है वह ‘एहतिकार’ यानी जमाख़ोरी है। ‘एहतिकार’ से मुराद मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों की बिक्री में इस अंदाज़ से रुकावट डालना कि लोग बाज़ार के आम भाव के मुक़ाबले में ज़्यादा क़ीमत देने पर मजबूर हो जाएँ। शरीअत में ‘एहतिकार’ की मनाही की गई है और वर्तमान सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ‘एहतिकार’ में लिप्त व्यापारियों को इस हरकत से रोके और अपने रेगूलेटरी regulatory अधिकार से काम लेकर जमाख़ोरी करनेवालों के काम में हस्तक्षेप करे और उनको इस हरकत से बाज़ रखे।
‘एहतिकार’ की मनाही में अनेक हदीसें आई हैं जिनको बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में दर्ज किया है। ‘एहतिकार’ के विषय पर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की चर्चाओं का सारांश यह है कि खाने-पीने की चीज़ों की जमाख़ोरी ज़्यादा बड़ा अपराध है। इसकी रोक-थाम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसके विपरीत आम चीज़ों की जमाख़ोरी भी निषिद्ध है बशर्तिके उसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को कोई तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अपने-अपने दौर के हिसाब से यह निर्धारण करने की भी कोशिश की कि क्या-क्या चीज़ें मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल हैं और क्या-क्या चीज़ें मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं हैं। ज़ाहिर है कि इसका निर्धारण परिस्थितियों और ज़माने के हिसाब से ही होगा।
13. ‘तदलीस’
तेरहवीं चीज़ जिसकी मनाही है वह ‘तदलीस’ यानी misrepresentation है। यह भी जायज़ नहीं है। ‘तदलीस’ किसी चीज़ के ऐब को छिपाने को कहते हैं। यह जो अख़बारों में आता है अंग्रेज़ी क़ानून के अनुसार जैसा है और जहाँ है के आधार पर, यह भी ‘तदलीस’ में आता है। इसी तरह ख़रीदनेवाले होशयार हो जाओ का उसूल भी शरई रूप से जायज़ नहीं। यह कहना कि आप यह घड़ी ख़रीद लें, इसकी क़ीमत पाँच सौ रुपये है। जहाँ तक इसमें किसी ऐब या ख़राबी का सम्बन्ध है तो वह घड़ी ख़रीदते समय आप स्वयं देख लें। अगर बाद में कोई ख़राबी निकली तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, यह भी शरई रूप से जायज़ नहीं। अगर उसमें ख़राबी है तो आपको बताना चाहिए और अगर यह ख़राबी बड़ी निकल आए तो आपको वापस लेना चाहिए। ख़राबी को छिपाकर चीज़ को बेच देना और ज़िम्मेदारी ख़रीदार पर डाल देना, यह शरीअत में जायज़ नहीं है। इस तरह के जितने विज्ञापन छपते हैं सब ग़लत और ग़ैर-क़ानूनी हैं। किसी को अधिकार नहीं कि दोष छिपाने का अधिकार अपने पास रखे और दूसरे को वह त्रुटिपूर्ण चीज़ लेने पर मजबूर करे।
14. ‘ख़लाबा’
चौधवीं चीज़ जिसकी मनाही है वह ‘ख़लाबा’ है। ‘ख़लाबा’ कहते हैं ऐसे कारोबारी हथकंडों को जिनके द्वारा आदमी चापलूसी या तेज़ कलामी के ज़रिये दूसरे को प्रभावित कर दे। कभी-कभी लोग इतने तेज़-तर्रार और चालबाज़ होते हैं कि सीधे-सादे आदमी को प्रभावित कर देते हैं। इसको ‘ख़लाबा’ कहते हैं। यानी कोई आदमी किसी कारोबारी की चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित होकर ग़लत चीज़ ख़रीद ले और अपने पैसे नष्ट कर दे। इसका आधार एक प्रसिद्ध हदीस पर है जिसको हदीसे-ख़लाबा कहते हैं।
एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो सीधा-सादा आदमी हूँ। बाज़ार जाता हूँ तो दुकानदारों की बातों से प्रभावित होकर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ और जब घर आता हूँ तो पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने फ़रमाया कि जब आइन्दा तुम कोई क्रय-विक्रय करो तो कहो कि “मैं किसी धोखे से प्रभावित नहीं होऊँगा और मुझे इस मामले में तीन दिन तक फ़ैसले का अधिकार होगा। अगर मैं चाहूँगा तो तीन दिन के अन्दर इसको वापस कर सकता हूँ।” इसी से वह उसूल निकला जिसको इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) ‘ख़ियार’ के शब्द से परिभाषित करते हैं यानी options. इनपर अभी बात करता हूँ। आख़िरी चीज़ जिसकी मनाही है वह नाजायज़ चीज़ों का कारोबार है। मैं एक चर्चा में ‘माले-मुतक़व्विम’ और ‘ग़ैर-मुतक़व्विम’ पर कुछ विस्तार से बात कर चुका हूँ। कारोबार के लिए ज़रूरी है कि वह माल ‘मुतक़व्विम’ के आधार पर हो। ‘माले-ग़ैर-मुतक़व्विम’ अगर मबीअ (बेचा गया) हो तो ‘बैअ’ बातिल और निरस्त है। ‘माले-ग़ैर-मुतक़व्विम’ अगर समन
हो तो ‘बैअ’ फ़ासिद (अवैध) है।
15. ‘ख़ियारात’
अभी ‘ख़ियारात’ की बात हुई थी। ‘ख़ियार’ का उसूल सबसे पहले इस्लामी शरीअत ने क़ानून एवं व्यापार जगत् में परिचित कराया। विकल्प बहुत सारी क़िस्मों के होते हैं। हर व्यक्ति को फ़िक़्ही आदेशों में बयान की गईं इन विस्तृत शर्तों के साथ इस तरह के विकल्प रखने का अधिकार है जिनमें से ‘ख़ियार’ शर्त है। इसका उदाहरण अभी मैंने दे दिया है।
एक ‘ख़ियारे-ऐब’ है। इससे मुराद यह है कि अगर ख़रीदारी और क़ब्ज़े के बाद सौदे में कोई ऐसा ऐब निकल आया जो विक्रेता के यहाँ से ही चीज़ में मौजूद था, तो ख़रीदार को तीन दिन तक अधिकार है कि चाहे तो चीज़ को अपने पास रखे और चाहे तो सौदा निरस्त कर दे। एक ‘ख़ियारे-रूयत’ है कि अगर आपने बिना देखे चीज़ ख़रीद ली। उदाहरणार्थ कराची में किसी के साथ मकान की ख़रीदारी का मामला कर लिया और रक़म भी आपने दे दी। लेकिन आप ‘ख़ियारे-रूयत’ के तहत मकान देखने के बाद सौदा निरस्त भी कर सकते हैं। यह ‘ख़ियारे-रूयत’ कहलाता है।
एक ‘ख़ियारे-मजलिस’ होता है कि किसी मजलिस में एक मामला हुआ तो उस समय तक आप उसपर पुनर्विचार कर सकते हैं जब तक कि आप उस मजलिस में हैं।
एक ‘ख़ियारे-तअय्युन’ होता है कि किसी स्टोर में एक जैसी तीन गाड़ियाँ खड़ी थीं। आपने एक ख़रीद ली और पैसे दे दिए। अब उनमें से कौन-सी आप लेना चाहेंगे यह आपका अधिकार है। बेचनेवाला यह नहीं कह सकता कि आप यह गाड़ी लें और वह न लें। अगर एक तरह की बहुत-सी चीज़ें हैं। आपने उनमें से एक की क़ीमत अदा कर दी और यह निर्धारण नहीं हुआ कि आप कौन-सी लेंगे तो आपकी मर्ज़ी है कि उनमें से कोई एक पसन्द कर लें। बेचनेवाले को अधिकार नहीं कि आपको एक ख़ास चीज़ लेने पर मजबूर करे।
एक ख़ियारे-नक़्द है, कि आपने एक ऐसे इलाक़े में कोई चीज़ ख़रीद ली जहाँ एक से अधिक सिक्के चलते हैं। उदाहरणार्थ कुछ देशों में डॉलर भी चलता है और अपना सिक्का भी चलता है। हमारे यहाँ ब्लोचिस्तान के कुछ इलाक़ों में ईरानी करंसी भी चलती है और पाकिस्तानी सिक्का भी चलता है। अफ़ग़ानिस्तान के अधिकतर इलाक़ों में पाकिस्तानी रुपया भी चलता है, अफ़ग़ानी सिक्का भी चलता है और डॉलर भी चलता है। तो वहाँ दोनों पक्षों को सिक्का तय करने का अधिकार है।
ये कुछ संक्षिप्ततम आदेश हैं जो शरीअत ने व्यापार और कारोबारी लेन-देन के बारे में दिए हैं। उनमें से हर एक का ज़िक्र मैंने मात्र शीर्षक के तौर पर किया है। ये ‘ख़ियारात’ जो मैंने बताए हैं उनमें से हर एक पर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने अलग-अलग किताबें लिखी हैं। ख़ियारे-शर्त, ख़ियारे-ऐब और इस तरह हर ख़ियार पर अलग-अलग किताबें मौजूद हैं। इससे अनुमान होगा कि यह कितना विस्तृत ज्ञान है और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसपर कितना ग़ौर किया है।
सवालात
सवाल : हाउसिंग स्कीमों के प्लॉट्स बनाने से पहले ही बिकने लगते हैं, बल्कि लोग ऐडवांस में फ़ार्म बेचते हैं। क्या यह दुरुस्त नहीं हैं?
जवाब : अगर किसी हाउसिंग स्कीम में प्लानिंग हो गई है और आपके नाम कोई निर्धारित प्लाट अलाट हो गया और उसके काग़ज़ात आपको मिल गए हैं तो इसको आप बेच सकते हैं। यह आपकी मिल्कियत के समान है। लेकिन अगर अभी वहाँ प्लाटिंग नहीं हुई और आपका मिल्कियती प्लाट निर्धारित नहीं हुआ तो उसको आगे बेचना जायज़ नहीं है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी बनी थी जो इधर बहरिया टाउन के क़रीब थी। वहाँ समष्टीय रूप से तो सोसाइटी की ज़मीन निर्धारित है। उसकी बहुत-सी क़िस्तें भी लोगों ने दे दी हैं, लेकिन अभी तक बहरिया फ़ाउंडेशन ने प्लानिंग करके निर्धारित नहीं किया कि यह हिस्सा इस्लामी यूनिवर्सिटी का है और यह किसी और का है। अत: वहाँ व्यक्तियों का अलग-अलग हिस्सा भी निर्धारित नहीं हुआ। ऐसा प्लाट बेचना जायज़ नहीं है। इसलिए कि न वह ज़मीन अभी तक मेरी मिल्कियत में आई है और न मेरे क़ब्ज़े में है और न ही काग़ज़ात मुझे मिले हैं, न वह मेरी मिल्कियत है। जब मेरा हिस्सा निर्धारित हो जाएगा कि यह प्लाट नम्बर मेरा है और उसकी फ़ाइल मेरे हाथ में आ जाए तो वह बेचना जायज़ होगा। इसलिए कि काग़ज़ात का क़ब्ज़े में आना प्लाट के क़ब्ज़े में आने के समान है। प्लाट के गले में तो आप ज़ंजीर बाँधकर नहीं रखेंगे। न उसको अलमारी में रख सकते हैं। प्लाट का क़ब्ज़ा उसके काग़ज़ात पर क़ब्ज़े से समझा जाता है। या तो उसकी दस्तावेज़ आपके हाथ में आ गई या आपने दीवार बनाकर चौकीदार रख दिया। दोनों स्थितियों में आपका क़ब्ज़ा पूरा हो गया है।
☆
सवाल : नाजायज़ तिजारतों की क़िस्मों में प्राइज़ बांड्ज़ किस कैटेगरी में आते हैं?
जवाब : प्राइज़ बांड में ‘क़िमार’ भी है, ‘रिबा’ भी है और ‘मैसिर’ तो अवश्य ही है।
☆
सवाल : बैंक या विभिन्न कंपनियों से जो शेयर्ज़ ख़रीदे जाते हैं क्या वे जायज़ हैं?
जवाब : शेयर्ज़ ख़रीदे जाने की तीन शर्तें हैं। याद रखें कि ये तीन शर्तें पूरी होती हों तो शेयर्ज़ ख़रीदना जायज़ है। और नहीं हैं तो नाजायज़ है।
पहली शर्त यह है कि जिस कंपनी के शेयर्ज़ ख़रीदे जा रहे हैं वह कंपनी जायज़ कारोबार कर रही हो।
दूसरी शर्त यह है कि जिस कंपनी के शेयर्ज़ ख़रीदे जा रहे हैं उस कंपनी के पास tangible physical assests मौजूद हों।
तीसरी शर्त यह है कि शेयर्ज़ की फ़्यूचर सेल न की जाए। अगर तीनों शर्तें हों तो शेयर्ज़ का क्रय-विक्रय जायज़ है।
☆
सवाल : मुशारका की परिभाषा बता दें। क्या लाभ-हानि की साझेदारी पर जो लोग बैंक से लाभ लेते हैं वह ब्याज होगा?
जवाब : मुशारका की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक आदमी मिलकर पैसा लगाएँ। उनमें से कुछ या सब मिलकर इस कारोबार का प्रबन्ध करें और जो लाभ हो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार वितरित हो। और अगर घाटा हो तो लोगों की रक़्मों के बराबर हो। सिद्धान्त यह है कि लाभ होगा तो वे आपस की शर्तों के अनुसार तय किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आपने पचास रुपये लगाए। दूसरे ने पच्चीस रुपये लगाए, तीसरे ने बीस लगाए और चौथे व्यक्ति ने पाँच रुपये लगाए। जिसने पाँच रुपये लगाए हैं, वह कारोबार का माहिर है जबकि आप कारोबार के माहिर नहीं हैं। अब वह यह कह सकता है कि मेरी रक़म तो पाँच रुपये है, लेकिन मैं लाभ में सबको बराबर रखूँगा और सब पच्चीस-पच्चीस रुपये लाभ लेंगे। यह करना जायज़ है। इसलिए कि हो सकता है जिसने पचास रुपये लगाए हैं वह कारोबार का माहिर न हो। जिसने पाँच लगाए हैं वह माहिर है। इसलिए उसूल यह है कि “लाभ का निर्धारण उन शर्तों पर होगा जो दोनों या सभी पक्षों ने तय की हैं और अगर घाटा होगा तो जिसने जितना पैसा लगाया है उसके अनुसार नुक़्सान में हिस्सेदार होगा।” जिसने पाँच प्रतिशत पैसा लगाया है उसका पाँच प्रतिशत नुक़्सान होगा और जिसने पच्चीस प्रतिशत लगाया है उसका पच्चीस प्रतिशत नुक़्सान होगा।
☆
सवाल : जो लोग लाभ-हानि के आधार पर बैंकों से लाभ लेते हैं क्या वह सचमुच लाभ है या ‘रिबा’ है?
जवाब : बैंक से मिलनेवाला लाभ वर्तमान परिस्थितियों में तो ‘रिबा’ ही के क़रीब-क़रीब है। क्योंकि बैंक जो आगे रुपया दे रहा है वह लाभ-हानि पर नहीं दे रहा, बल्कि निर्धारित और गारंटी प्राप्त लाभ पर दे रहा है। अगर बैंक आगे भी वह रक़म लाभ-हानि की साझेदारी पर दे रहा है तो ठीक है। लेकिन बैंक यह करते हैं कि आपसे जो रुपया लेते हैं उसको आगे ब्याज पर देते हैं। उदाहरणार्थ दस प्रतिशत अगर वह ब्याज लेता है तो पाँच प्रतिशत आपको देगा और पाँच प्रतिशत स्वयं रखेगा। यह बैंकों के कारोबार का आम अंदाज़ है। यह जायज़ नहीं। जो बैंक आगे भी बिना ब्याज के पैसे देते हैं उनमें आप पूँजी लगा सकते हैं। अत: जो इस्लामी बैंकिंग है, जो कमर्शियल बैंक हैं उनमें से कुछ बैंकों ने इस्लामी बैंकिंग शुरू कर रखी है। वे जायज़ हैं। यह आपको अलग-अलग चेक करना पड़ेगा कि किस बैंक का कारोबार शरीअत के अनुसार है और किसका नहीं।
☆
सवाल : क्या इंशोरेंस नाजायज़ है?
जवाब : इंशोरेंस में जो कोऑपरेटिव इंशोरेंस है उसकी अधिकतर शक्लें जायज़ हैं। जो दूसरा इंशोरेंस है उसकी अधिकतर शक्लें नाजायज़ हैं। लेकिन इंशोरेंस की तमाम क़िस्मों को जायज़ या तमाम क़िस्मों को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। आपको अलग-अलग पता करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव इंशोरेंस की अक्सर शक्लें जायज़ हैं। और जो दूसरा इंशोरेंस है उसकी अधिकांश क़िस्में नाजायज़ हैं।
☆
सवाल : अगर किसी ज़मीन पर किसी का नाजायज़ क़ब्ज़ा हो, तो क्या इस ज़मीन को किसी व्यक्ति के हाथ इस शर्त पर बेचा जा सकता है कि वह क़ब्ज़ा स्वयं छुड़ा ले और उसकी सेवा के बदले उससे क़ीमत कम ली जाए?
जवाब : मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख़याल है कि यह जायज़ नहीं है। इसमें यह किया जा सकता है कि पहले आप उस व्यक्ति को क़ब्ज़ा छुड़ाने में अपना वकील बना दें। आप बेशक उसके साथ वादा कर लें कि आप यह ज़मीन उसको बेच देंगे। और जब वह आपके वकील की हैसियत से क़ब्ज़ा प्राप्त कर ले तो आप उसको बेच दें। यह शक्ल ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। बाक़ी मैं इसके वैध या अवैध होने के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मुझे इसमें कुछ संकोच महसूस होता है।
☆
सवाल : क्या स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार किया जा सकता है?
जवाब : अभी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं या कोटेड शेयर्ज़ हैं वे इन तीन शर्तों के साथ जायज़ हैं जिनका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ।
☆
सवाल : हमारी बैंकिंग व्यवस्था में ‘रिबा’ की निशानदेही कर दें कि किस तरह इससे बचा जा सकता है?
जवाब : ‘रिबा’ की निशानदेही तो मैंने कर दी। या तो आप अपना रुपया करंट अकाउंट में रखें। उसमें ‘रिबा’ नहीं है। यह नहीं करना चाहते तो सेफ़ डिपाज़िट में जाकर रख लें। यह भी जायज़ है। सेफ़ डिपाज़िट किराए पर लेना भी जायज़ है। अगर ये दोनों सम्भव न हों तो इस्लामी बैंकिंग की ब्राँचें हर जगह खुल रही हैं। वहाँ रुपया रखें। वहाँ भी सम्भव न हो तो कम-से-कम इतना कर लें कि पीएलएस एकाउंट में रखें। पीएलएस अकाउंट पर भी बड़ी आपत्तियाँ हैं लेकिन यह कम-से-कम शेष चीज़ों से बेहतर है।
☆
सवाल : जिस अकाउंट में फ़िक्स डिपाज़िट पर रक़म रखी हो उसका लाभ जायज़ है कि नाजायज़?
जवाब : मेरे ख़याल में तो यह ‘रिबा’ की एक शक्ल है और नाजायज़ है।
✩
सवाल : क्या इंशोरेंस करना ग़लत और नाजायज़ है?
जवाब : मैंने अभी बताया है कि पारम्परिक इंशोरेंस की अधिकतर शक्लें नाजायज़ हैं, और कोऑपरेटिव इंशोरेंस की अधिकतर शक्लें जायज़ हैं।
☆
सवाल : बाज़ार में जो इनामी स्कीमें निकलती हैं, जैसे कि आपने उदाहरण दिया, और कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ख़रीदता है, लेकिन न कूपन भरता है और न स्कीम में हिस्सा लेता है और न ही इनाम लेना चाहता है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है?
जवाब : मेरे ख़याल में इनामी स्कीमों से बचते हुए मात्र कमोडिटी ख़रीदना जायज़ है। आपको एक ख़ास चीज़ ख़रीदनी और हो आपको उस ख़ास कमोडिटी में दिलचस्पी हो तो ले लें, इसमें मुझे कोई बुराई मालूम नहीं होती।
☆
सवाल : कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है कि लूडो खेलना भी जुए की एक शक्ल है।
जवाब : नहीं, लोडू खेलना जुए की शक्ल नहीं है। अगर इसमें हार जीत पर पैसा लगाया है तो फिर यह जुआ है और अगर पैसा नहीं लगाया तो फिर तो कोई भी खेल जुआ नहीं है। जो खेल खेलना चाहें, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, अगर उसमें पैसा लगाया है कि जीतनेवाले को इतने रुपये मिलेंगे और हारनेवाले को नहीं, तो यह ‘क़िमार’ या जुआ है। लेकिन अगर पैसा नहीं लगाया है तो जायज़ है।
✩
सवाल : Is medical insurance allowed?
जवाब : इसका भी वही सिद्धान्त है कि अगर इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी रिबा, ‘क़िमार’ और ‘ग़रर’, तो नाजायज़ और अगर नहीं पाई जातीं तो जायज़ होगा।
☆
सवाल : विरासत का विभाजन या वितरण जब होता है तो उस समय तो प्रमुख मर चुका होता है। तो बादवाले धन-दौलत को वितरित करते हैं। तो ग़लत वितरण की सज़ा मरनेवाले को क्यों मिलेगी?
जवाब : यह किसने कहा है कि मरनेवाले को सज़ा मिलेगी नहीं, मरनेवाले को दूसरों की कोताही की कोई सज़ा नहीं होगी। यह किसने कहा कि मरनेवाले को सज़ा मिलेगी? मरनेवाला तो चला गया। अगर वारिसों में किसी ने विरासत को शरीअत के अनुसार वितरित नहीं होने दिया तो ग़लती उसने की। जिसने भी ऐसा किया सज़ा उसको मिलेगी। वह मरनेवाला हो या मरनेवाले के बाद ऐसा करनेवाला।
☆
सवाल : आपने कहा कि जो कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई उसके शेयर्ज़ ख़रीदना जायज़ नहीं। क्या वह कंपनी जो चल रही है और उसकी और मार्केट इस्टेक सबको मालूम हो, उसमें शेयर्ज़ ख़रीदे जा सकते हैं?
जवाब : मैंने यह कहा है कि अगर कोई कंपनी अभी लॉन्च हुई है और उसके पास केवल liquidity है और tangible assests नहीं हैं। इसके शेयर्ज़ ख़रीदने का अर्थ यह है कि ज़र का क्रय-विक्रय ज़र के मुक़ाबले में हो रहा है जो अगर उधार या कमी-बेशी के साथ हो तो शरीअत में जायज़ नहीं है। शरीअत में रुपये पैसे का क्रय-विक्रय रुपये पैसे के साथ इस स्थिति में जायज़ है जब on the spot हो और par value पर हो। हदीस में आया है “हाथ-दर-हाथ और बराबर-बराबर।”
इसलिए अगर इसमें हाथ-दर-हाथ न हो या बराबर-सराबर पार वैल्यू (par value) न हो तो जायज़ नहीं है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर पार वैल्यू पर ख़रीद रहे हैं तो यह हर स्थिति में जायज़ है, शर्त यह है कि कारोबार जायज़ हो। लेकिन अगर उस कंपनी के tengible assests नहीं हैं तो इसका शेर पार वैल्यू के अलावा नहीं ख़रीदा जा सकता। पार वैल्यू पर न ख़रीदने का अर्थ यह है कि आप दस रुपये छः रुपये में ले रहे हैं या दस रुपये बारह रुपय में ले रहे हैं तो ये दोनों शक्लें जायज़ नहीं हैं।
☆
सवाल : अक्सर शब्दावलियाँ समझ में नहीं आतीं, तो आप क्या लिखवा देते हैं। ज़्यादातर हम स्वयं लिखते हैं। कृपा करके आप मुश्किल शब्दावलियों को बोर्ड पर लिख दिया करें।
जवाब : यह बात तो आपको पहले दिन कहनी चाहिए थी। अब तो दस दिन गुज़र गए हैं। कल और परसों इंशा अल्लाह कोई मुश्किल बात नहीं होगी।
☆
सवाल : मकान किराए पर देकर हम हर महीने बिना किसी मेहनत के किराया वुसूल करते हैं और मकान भी वैसे का वैसा वापस मिल जाता है। इस तरह बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं हर माह लाभ लेते हैं और समय आने पर पूरी-की-पूरी रक़म भी मिल जाती है। तो इन दोनों में अन्तर क्या हुआ?
जवाब : आपने मेरी बात ग़ौर से नहीं सुनी। मैंने दो बार इसको स्पष्ट किया था। मैंने कहा था कि जब आप किसी से कोई चीज़ लेती या देती हैं, तो वह चीज़ दो में से कोई एक तरह की होगी। या तो वह होगी जो आपको वही चीज़ वापस मिल जाएगी। जैसे मैंने क़लम, किताब, गाड़ी साइकिल का उदाहरण दिया था। ये चीज़ें इस्तेमाल के बाद आपको मिल जाती हैं। वही चीज़ मिलती है जो आपने दी थी।
कुछ चीज़ें वे हैं जो आप इस्तेमाल करके समाप्त कर देते हैं और फिर इस तरह की एक और चीज़ वापस देते हैं। उस और उस जैसी में बहुत अन्तर है। ज़मीन-आसमान का अन्तर है। जब आपने मकान किराए पर दे दिया तो वही मकान आप को मिल गया। कोई और मकान नहीं मिला। यह नहीं होता कि आपने ‘एफ़ एट’ में मकान किराए पर लिया और जब किराएदार ने ख़ाली किया तो ‘एफ़ टेन’ वाला मकान आपको दे दिया। यह किराएदारी नहीं है।
जब आपने चीनी दी, या पैसा दिया, तो आपको वही चीनी या वही पैसा वापस नहीं मिलेगा। वह तो ख़र्च होकर कहीं-का-कहीं चला गया। वह चीज़ तो समाप्त हो गई। अब आपको उस जैसी रक़म या उस जितनी चीनी वापस मिलेगी। वह चीज़ नहीं मिलेगी जो आपने दी है। दोनों में ज़मीन-आसमान का अन्तर है। दोनों का आदेश एक नहीं हो सकता।
☆
सवाल : क्या स्टॉक एक्सचेंज में पूँजी निवेश करना हराम है?
जबाव : अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर वह कारोबार उक्त शर्तों पर पूरा उतरता है तो जायज़ है वरना नहीं।
☆
सवाल : पाकिस्तान में कौन से बैंक ब्याज मुक्त हैं?
जवाब : मेरे ख़याल में अभी तक तो केवल मीज़ान बैंक ब्याज मुक्त है। कुछ और बैंक भी
क़ायम होनेवाले हैं।
☆
सवाल : इस्लामिक फ़ाइनांशियल स्कीम की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
जवाब : हमने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक बैंकिंग ऐंड फ़ाइनांस का एक अलग विभाग शुरू किया है। इसमें एमएससी होता है। आप चाहें तो आकर एमएससी कर सकते हैं।
✩
सवाल : मैंने दस वर्ष के लिए अपने बेटे की ख़ातिर डिफ़ेंस सर्टिफ़िकेट्स ख़रीदे हैं, क्या वे जायज़ हैं?
जवाब : अफ़सोस है कि वे जायज़ नहीं हैं। बेहतर यह होता कि आप कोई मकान ख़रीद कर किराए पर दे देते। आपके मकान की क़द्रो-क़ीमत बढ़ती और आपको किराया भी मिलता। मकान नहीं तो कोई दुकान ख़रीद लें। यह एक tangible assest है जो मौजूद रहेगा। इसमें ‘रिबा’ का ख़तरा भी नहीं है और सम्पत्ति की क़ीमत हर जगह बढ़ती रहती है और पैसे की क़ीमत घटती रहती है। इसलिए वह चीज़ लें जिसमें दीन का भी फ़ायदा हो और दुनिया का भी फ़ायदा हो।
Recent posts
-

फ़िक़्हे-इस्लामी आधुनिक काल में (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 12)
17 April 2025 -

मुसलमानों का अद्वितीय फ़िक़ही संग्रह एक विश्लेषण (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 11)
17 April 2025 -

अपराध और सज़ा का इस्लामी क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 9)
22 March 2025 -

इस्लाम का संवैधानिक और प्रशासनिक क़ानून (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 8)
17 March 2025 -

शरीअत के उद्देश्य और इज्तिहाद (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 7)
16 March 2025 -

इस्लामी क़ानून की मौलिक धारणाएँ (फ़िक़्हे इस्लामी: लेक्चर 6)
27 February 2025