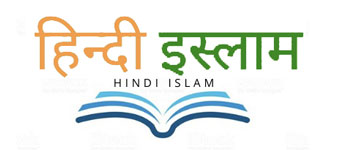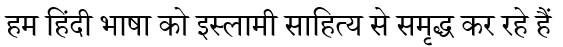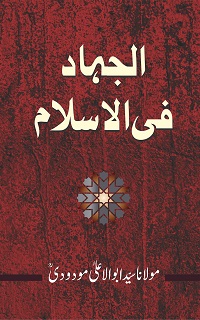
इस्लाम में जिहाद: क्या और क्यों?
-
सामयिकी
- at 12 December 2023
लेखक: सय्यिद अबुल आला मौदूदी
अनुवाद और प्रस्तुति: हिन्दी इस्लाम डॉट कॉम (HindiIslam.com)
उर्दू पुस्तक: जिहाद फिल इस्लाम
पहली प्रकाशन: 1930 (दारुल मुसन्नेफीन, आज़मगढ़, यूपी)
परिशिष्ट: सेप्तेंबर 2023 (हिन्दी इस्लाम डॉट कॉम )
सूची
प्रस्तावना
पहला अध्याय : इस्लामी जिहाद की वास्तविकता
मानव जीवन का सम्मान
दुनिया पर इस्लामी शिक्षा का नैतिक प्रभाव
न्यायोचित हत्या
न्यायोचित और अन्यायपूर्ण हत्या के बीच अंतर
अपरिहार्य रक्तपात
सामुदायिक बिगाड़
युद्ध, एक सामाजिक और नैतिक दायित्व
युद्ध का औचित्य
अल्लाह के मार्ग में जिहाद
सत्य और असत्य की सीमा
अल्लाह के मार्ग में जिहाद की उत्कृष्टता
जिहाद की उत्कृष्टता का कारण
सभ्यता के प्रयोजन में जिहाद का महत्व
दूसरा अध्याय : रक्षात्मक युद्ध
रक्षात्मक युद्ध की धार्मिक बाध्यता
रक्षात्मक युद्ध के विभिन्न रूप
(1) क्रूरता और आक्रामकता का जवाब
(2) सत्य मार्ग का संरक्षण
(3) छल और वचन-भंग का दंड
(4) गुप्त आंतरिक शत्रु का दमन
(5) शांति की रक्षा
(6) कमज़ोरों और दमितों की सहायता
रक्षा का उद्देश्य
तीसरा अध्याय : सुधार के लिए युद्ध
सामुदायिक दायित्व की नैतिक अवधारणा
सामुदायिक दायित्व से जुड़ी इस्लाम की उच्च शिक्षा
भलाई का आदेश देने और बुराई को रोकने’ की वास्तविकता
सामूहिक जीवन में भलाई के आदेश और बुराई के निषेध की अवधारणा की स्थिति
भलाई के आदेश और बुराई के निषेध का अंतर
बुराई से रोकने की कार्यप्रणाली
षडयंत्र और बिगाड़ के ख़िलाफ़ युद्ध
षडयंत्र (फ़ितना) की जांच
बिगाड़ (फ़साद) की जांच
षडयंत्र और बिगाड़ को मिटाने के लिए ईश्वरीय आदेशों पर आधारित व्यवस्था की ज़रूरत
सशस्त्र प्रितरोध का आदेश
युद्ध का कारण और उद्देश्य
जिज़्या की वास्तविकता
इस्लाम और साम्राज्यवाद
इस्लामी विजयों का वास्तविक कारण
चौथा अध्याय : इस्लाम का प्रसार और तलवार
धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं
इस्लाम के आह्वाण और उपदेश का मूल सिद्धांत
मार्गदर्शन और गुमराही का रहस्य
इस्लाम के प्रसार में तलवार की भूमिका
पांचवां अध्याय : शांति और युद्ध के इस्लामी क़ानून
(1) युद्ध के पूर्व-इस्लामी, अरब तरीक़े
युद्ध की अरबी अवधारणा
अरबों के चरित्र पर सशस्त्र संघर्ष की आवृत्ति का प्रभाव
युद्ध के कारक
विजय-धन की चाहत
गौरव
प्रतिशोध
युद्ध में बर्बरता
ग़ैर-लड़ाकों पर हमला
आग की पीड़ा
युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार
अप्रत्याशित आक्रमण
मृतकों का अपमान
विश्वासघात
(2) रोम और ईरान की युद्ध पद्धतियाँ
धार्मिक अत्याचार
दूतों पर अत्याचार
विश्वासघात
युद्ध में बर्बरता
युद्धबंदियों की स्थिति
(3) इस्लामी सुधार
युद्ध की इस्लामी अवधारणा
युद्ध के उद्देश्य में सुधार
युद्ध की पद्धति में सुधार
ग़ैर-लड़ाकों का सम्मान
लड़ाकों के अधिकार
अप्रत्याशित हमले का निषेध
आग में जलाने का निषेध
बंधे हुए क़ैदी को मारने का निषेध
लूट-मार का निषेध
विनाश का निषेध
मृतकों के अंगभंग का निषेध
बंदी-हत्या का निषेध
दूत की हत्या का निषेध
वचनभंग का निषेध
अव्यवस्था का निषेध
शोर और हंगामे का निषेध
बर्बर कृत्यों के ख़िलाफ़ सामान्य निर्देश
सुधार के परिणाम
(4) युद्ध के सभ्य क़ानून
कमांडरों के प्रति निष्ठा
शपथ और समझौतों का सम्मान
तटस्थ पक्ष के अधिकार
युद्ध की घोषणा
युद्धबन्दी
ग़ुलामी की समस्या
युद्ध की लूट की समस्या
संघर्षविराम और शरण
विजित राष्ट्रों के साथ मामला
दो प्रकार के विजित
संधि राज्य
ग़ैर-संधि वाले राज्य
ज़िम्मियों (इस्लामी राज्य के ग़ैरमुस्लिम नागरिकों) के सामान्य अधिकार
ज़िम्मियों के पहनावे का सवाल
(5) कुछ अपवाद
बनु नज़ीर का निष्कासन
बनू क़ुरैज़ा की घटना
काब बिन अशरफ की हत्या
ख़ैबर के यहूदियों का निष्कासन
नजरान के लोगों का निष्कासन
(6) युद्ध के आधुनिक क़ानूनों की स्थापना
छठा अध्याय : अन्य धर्मों में युद्ध की स्थिति
धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के सिद्धांत
विश्व के चार प्रमुख धर्म
(1) हिन्दू धर्म
हिंदू धर्म के तीन युग
वेदों में युद्ध की शिक्षा
ऋग्वेद
यजुर्वेद
सामवेद
अथर्ववेद
वेदों की युद्ध से जुड़ी शिक्षाओं पर एक नज़र
गीता का युद्ध दर्शन
गीता के दर्शन पर एक नज़र
मनु के युद्ध के नियम
युद्ध का उद्देश्य
युद्ध की नैतिक सीमाएँ
विजित राष्ट्रों के साथ व्यवहार
वंश-आदारित भेदभाव
(2) यहूदी धर्म
युद्ध का उद्देश्य
युद्ध की सीमा
(3) बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के स्रोत
अहिंसा की शिक्षा
बौद्ध दर्शन
बौद्ध धर्म की वास्तविक कमज़ोरी
बौद्ध अनुयायियों के जीवन पर अहिंसा का प्रभाव
(4) ईसाइयत
ईसाइयत के स्रोतों की जांच
“प्रेम” की शिक्षा
ईसाइयत में नैतिकता का दर्शन
ईसाई नैतिकता में मुख्य दोष
मसीह के आह्वाण की वास्तविकता
ईसाइयत में युद्ध न होने का कारण
ईसाई और यहूदी धर्मविधानो का संबंध
धर्मविधानो और ईसाइयत का पृथक्करण:
ईसाई चरित्र पर अलगाव का प्रभाव
(5) चारों धर्मों की शिक्षाओं पर एक नज़र
सातवां अध्याय : आधुनिक सभ्यता में युद्ध
(1) युद्ध का नैतिक पहलू
महायुद्ध के कारण
राष्ट्रों की गुटबंदी
युद्ध की शुरुआत
युद्ध के भागीदारों के लक्ष्य और उद्देश्य
गोपनीय समझौते
युद्ध के बाद देशों का विभाजन
युद्ध के वैध उद्देश्य
शांति स्थापना और निरस्त्रीकरण प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र
आधुनिक निरस्त्रीकरण प्रस्ताव
(2) युद्ध का व्यावहारिक पक्ष
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की वास्तविकता
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के तत्व
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का अस्थायित्व
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का सामरिक विभाग
युद्ध के नियमों का अर्थ
युद्ध की अनिवार्यताओं का प्रचलित क़ानून
प्रदर्शन और वास्तविकता में अंतर
सैन्य और क़ानूनी समूहों की असहमति
(3) पश्चमी युद्ध क़ानूनों का सैद्धांतिक स्वरूप
युद्ध के नियमों का इतिहास
हेग समझौतों की वैधता
(4) युद्ध के आदेश और नियम
युद्ध की घोषणा
लड़ाके और ग़ैर-लड़ाके
सेनानियों के अधिकार और दायित्व
युद्ध के नियमों की बाध्यता
युद्धविराम
युद्धबंदी
घायल, बीमार और मृतक
घातक पदार्थों का उपयोग
जासूस
युद्ध में छल
प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां
ग़ैर-लड़ाकों के अधिकार और दायित्व
ग़ैर-लड़ाकों का पहला दायित्व
ग़ैर-लड़ाकों का सम्मान
असुरक्षित आबादी पर गोलाबारी
विजित शहरों के बारे में आदेश
व्यवसाय और उसके नियम
विनाश
तटस्थों के अधिकार और दायित्व
तटस्थता का इतिहास
वर्तमान समय में तटस्थों की स्थिति
तटस्थों के प्रति युद्धरतों के दायित्व
युद्धरतों के प्रति तटस्थों के दायित्व
(5) विश्लेषण
(6) परिशिष्ट (नया)
अल्लाह के नाम से, जो अत्यन्त कृपाशील और बड़ा दयावान है।
प्रस्तावना
आधुनिक काल में यूरोप ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम पर जो निराधार आरोप लगाए हैं, उनमें सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस्लाम एक रक्तपिपासु धर्म है और अपने अनुयायियों को रक्तपात सिखाता है। इस आरोप में अगर कुछ सच्चाई होती, तो स्वभाविक रूप से यह आरोप उस समय लगाया जाता, जब इस्लाम की पाषाणभेदी तलवार ने इस धरती पर तहलका मचा रखा था, और वास्तव में दुनिया को यह संदेह हो सकता था कि उनकी ये विजयी कार्रवाइयां किसी ख़ूनी शिक्षा का परिणाम हों। लेकिन अजीब बात है कि इस बदनामी का जन्म इस्लाम के विकास के सूरज के डूब जाने के लम्बे समय बाद हुआ। इसके काल्पनिक साँचे में उस समय जान फूँकी गई जब इस्लाम की तलवार तो ज़ंग खा चुकी थी, मगर ख़ुद इस आरोप के लेखक, यूरोप की तलवार निर्दोषों के ख़ून से लाल हो रही थी और उसने दुनिया के कमज़ोर देशों को इस तरह निगलना शुरू कर दिया था, जैसे कोई अजगर छोटे-छोटे जानवरों को डसता और निगलता है।
अगर दुनिया में समझ होती तो वह पूछती कि जो लोग ख़ुद शांति और सद्भाव के सबसे बड़े दुश्मन हों, जिन्होंने ख़ून बहा-बहा कर धरती को रंगीन कर दिया हो, जो ख़ुद दूसरे देशों को लूट रहे हों, आख़िर उन्हें क्या अधिकार है कि इस्लाम पर वह आरोप लगाएं जिस का अभियोग ख़ुद उन पर लगाया जाना चाहिए? कहीं इस सारे ऐतिहासिक अनुसंधान और विद्वतापूर्ण चर्चा-परिचर्चा से उनकी मंशा यह तो नहीं कि दुनिया की उस नफरत और आक्रोश की बाढ़ की धारा इस्लाम की ओर फेर दें जिस के ख़ुद उनके अपने रक्तपात के ख़िलाफ़ उमड कर आने की आशंका है? मनुष्य की यह स्वाभाविक दुर्बलता है कि जब वह मैदान में पराजित होता है तो पाठशाला में भी पराजित हो जाता है। जिस की तलवार से पराजित होता है, उसकी क़लम का भी मुक़ाबला नहीं कर पाता। यही कारण है कि हर युग में दुनिया पर उन्हीं विचारों और मतों का वर्चस्व होता है, जो तलवारधारी हाथों की क़लम से प्रस्तुत किए जाते हैं। अतः इस मामले में भी यूरोप को पूरी दुनिया की आँखों पर पट्टी बाँधने में पूरी तरह से सफलता मिली और ग़ुलाम मानसिकता वाले राष्ट्रों ने इस्लामी जिहाद के बारे में उसके द्वारा पेश किए गए सिद्धांत को बिना किसी शोध और विचार के इस तरह स्वीकार कर लिया, जिस तरह किसी ईशवरीय प्रकाशना को भी न स्वीकार किया गया होगा।
पिछली और वर्तमान शताब्दियों में मुसलमानों द्वारा इस आपत्ति का बार-बार जवाब दिया गया है और इस विषय पर इतना कुछ लिखा गया है कि अब यह एक घिसा-पिटा विषय प्रतीत होता है। लेकिन इस प्रकार के जवाब लेखन में मैंने अक्सर यह दोष देखा है कि इस्लाम के हिमायती विरोधियों से भयभीत होकर ख़ुद ही अभियुक्तों के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और अपराधियों की तरह सफ़ाई देने लगते हैं। कुछ सज्जनों ने तो यहां तक किया कि अपने मुक़दमे को मज़बूत करने के लिए इस्लाम की शिक्षाओं और उसके क़ानूनों में ही संशोधन कर डाला, और जिन-जिन चीज़ों को उन्होंने भयानक समझा, उन्हें रिकॉर्ड पर से पूरी तरह से गायब कर दिया, ताकि विरोधियों की नज़र उन पर न पड़ सके। लेकिन जिन लोगों ने इतना कमज़ोर पक्ष नहीं लिया उनमें भी कम से कम यह दोष तो ज़रूर मौजूद है कि वे जिहाद और लड़ाई पर इस्लामी शिक्षाओं को पूरी स्पष्टता के साथ नहीं समझाते और कई पहलुओं को इस तरह अधूरा छोड़ जाते हैं कि इसमें संदेह के लिए बहुत जगह रह जाती है। ग़लतफ़हमियों को दूर करने के लिए अस्ल ज़रूरत यह है कि अल्लाह के लिए जिहाद करने और अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए लड़ने संबंधी इस्लाम की शिक्षाओं और उसके क़ानूनों को बिना किसी कमी-बेशी के उसी तरह बयान कर दिया जाए जिस तरह यह पवित्र क़ुरआन, पैग़म्बर (सल्ल.) (सल्ल.) की हदीसों और फ़िक़्ह (इस्लामी धर्मविधान) की किताबों में दर्ज हैं। उनमें से कुछ भी न घटाया जाए और न बढ़ाया जाए और न इस्लाम के मूल इरादे और उसकी शिक्षाओं की भावना को बदलने का कोई प्रयास किया जाए।
मैं सैद्धांतिक तौर पर इस से असहमति रखता हूं कि हम अपने विश्वासों और सिद्धांतों को दूसरों के दृष्टिकोण से अनुकूल बनाकर पेश करें। दुनिया में एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हों। प्रत्येक पक्ष का अपना दृष्टिकोण होता है और वह उसे ही सही मानता है। पवित्र क़ुरआन के अनुसार, प्रत्येक समुदाय के पास जो कुछ है वह उसी से खुश है। अत: दूसरों के दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने के लिए हम अपने सिद्धांतों और विश्वासों को कितना भी रंग कर पेश करें, यह असंभव है कि सभी अलग-अलग वैचारिक समूह हमसे सहमत हो जाएं और सभी को हमारा वह कृत्रिम रंग पसंद आ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि हम अपने धर्म की मान्यताओं और नियमों, उसकी शिक्षाओं और उसके क़ानूनों को उनके असली रंग में दुनिया के सामने पेश कर दें और उनके पक्ष में जो तर्क हम रखते हैं, उन्हें भी स्पष्ट रूप से बयान कर दें, फिर यह बात ख़ुद लोगों के विवेक पर छोड़ दें कि चाहे वे उन्हें स्वीकार करें या न करें। अगर वे इसे स्वीकार करते हैं, तो सौभाग्य, अगर वे नहीं करते हैं, तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं। यही अपनी मान्यताओं के प्रसार का सही सिद्धांत है, जिसे साहसी लोगों ने हमेशा अपनाया है, और ख़ुद अल्लाह के पैग़म्बरों ने भी इसी का पालन किया है।
इस ज़रूरत को मैं काफ़ी समय से महसूस कर रहा था, लेकिन मैं ज़रूरत की भावना से परे कार्रवाई की दिशा में कोई क़दम नहीं उठा सकता था, क्योंकि इस काम के लिए फ़ुर्सत की बहुत ज़रूरत होती है, और फ़ुर्सत ऐसी चीज़ है, जो एक पत्रकार को नहीं मिल पाती।
लेकिन दिसंबर 1926 के आखिरी दिनों में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे मुश्किलों की परवाह किए बिना कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या थी, जिसने अज्ञानी और अदूरदर्शी लोगों को इस्लामी जिहाद के बारे में झूठे विचारों को फैलाने का एक नया अवसर दे दिया, क्योंकि दुर्भाग्य से एक मुसलमान इस कृत्य को करने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया था और अख़बारों ने इस विचार को उससे जोड़ दिया था कि उसने अपने धर्म का दुश्मन समझ कर स्वामी को मार डाला था, और यह कि इस नेक काम को करने से वह स्वर्ग का उम्मीदवार था। सच्चाई तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन सामने जो आया वह यही घटना थी। इस वजह से इस्लाम के दुश्मनों के बीच एक उन्माद पैदा हो गया। उन्होंने इस्लामी विद्वानों की घोषणाओं और इस्लामी पत्रिकाओं और मुस्लिम नेताओं के सर्वसम्मत स्पष्टीकरणों के बावजूद इस घटना को उसकी भौतिक सीमा तक सीमित रखने के बजाय, पूरे मुस्लिम समुदाय तक फैला दिया और ख़ुद इस्लामी शिक्षाओं को इसका दोष देना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से पवित्र क़ुरआन पर आरोप लगाने लगे कि इसकी शिक्षा मुसलमानों को रक्तपिपासु और हत्यारा बनाती है, इसकी शिक्षा शांति और सुरक्षा के ख़िलाफ़ है। और इसकी शिक्षा ने मुसलमानों को इतना कट्टर बना दिया है कि वे हर अविश्वासी को हत्या का पात्र मानते हैं और उसे मार कर स्वर्ग जाने की आशा करते हैं। कुछ हद से बढ़े लोगों ने तो यहों तक कह दिया कि जब तक दुनिया में क़ुरआन की शिक्षा मौजूद है तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है, इसलिए सभी मनुष्यों को इस शिक्षा को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। इन झूठे विचारों को इतनी आवृत्ति के साथ प्रचारित किया गया कि सदबुद्धी रखने वाले लोगों के दिमाग़ भी भ्रमित हो गए और गांधीजी जैसे व्यक्ति ने, इससे प्रेरित होकर बार-बार इस विचार को व्यक्त किया:
“इस्लाम का जन्म ऐसे माहौल में हुआ, जहां निर्णायक ताक़त पहले भी तलवार थी और आज भी तलवार है।”
हालांकि ये सभी विचार किसी शोध और बौद्धिक खोज पर आधारित नहीं थे, बल्कि तोते की तरह उस पाठ को दोहराया जा रहा था, जो कभी उनके गुरू द्वारा सिखाया गया था। मगर एक असाधारण घटना ने इन भ्रमों को वास्तविकता का रंग दे दिया था, जिससे अज्ञानी लोग आसानी से धोखा खा सकते थे। इस तरह की आम ग़लतफ़हमी हमेशा इस्लाम के प्रसार के रास्ते में रुकावट होती हैं और ऐसे ही अवसर होते हैं, जिन में इस्लाम की सही शिक्षा को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की ज़रूरत होती है, ताकि धूल साफ़ हो जाए और सच्चाई का सूरज अधिक रोशनी के साथ उदय हो। इसलिए मैंने ख़ाली समय का इंतिज़ार करना बंद कर दिया और अख़बार के संपादन से बचने वाले उसी कम समय में इस विषय पर लेखन का काम शुरू कर दिया। साथ ही “अल-जमीअत” अख़बार के कॉलम में इसे प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया। आरंभ में, इरादा एक छोटा सा लेख लिखने का था, लेकिन बात छिड़ जाने के बाद, बहस के इतने आयाम सामने आते चले गए कि अख़बार के कॉलम में, उनका समाना मुश्किल हो गया। इसलिए 23-24 अंक प्रकाशित करने के बाद मुझे अख़बार में इसके प्रकाशन को रोकना पड़ा। अब मैं उस पूरी श्रृंखला को अंत तक पहुंचा कर एक किताब के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि यह किताब अधिकांश पहलुओं को अपने भीतर रखती है, फिर भी मुझे खेद है कि समय की कमी ने कई विषयों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर किया। इस किताब में, मैंने विशेष रूप से यह सावधानी बरती है कि कहीं अपने या दूसरे लोगों के व्यक्तिगत विचारों का हस्तक्षेप न हो। बल्कि सभी छोटे-बड़े मुद्दों को पवित्र क़ुरआन से लेकर प्रस्तुत किया है और जहाँ कहीं उनकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ी है, पैग़म्बर (सल्ल.) की हदीसों, इस्लामी धर्मशास्त्र की विश्वसनीय किताबों और सही और प्रामाणिक व्याख्याओं से मदद ली है। ताकि सभी को पता चल जाए कि आज दुनिया के रंग को देखकर कोई नयी चीज़ पैदा नहीं की गयी है, बल्कि जो कुछ कहा गया है वह अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम के विद्वानों की बातों पर आधारित है।
मैं उन सभी भाइयों से, जिनकी इस्लाम में आस्था नहीं है, और जो पूर्वाग्रह के आधार पर इस्लाम के प्रति अंध-विरोधी नहीं हैं, अनुरोध करता हूं कि वे इस किताब में इस्लाम की वास्तविक शिक्षा का अध्ययन करें और फिर हमें बताएं कि उन्हें इस शिक्षा पर क्या आपत्ति है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शंका है तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अबुल आला
दिल्ली
15 जून 1927
हिन्दी संस्करण की प्रस्तावना
मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की सर्वोत्कृष्ट कृति, ‘अल-जिहाद फ़िल-इस्लाम’ को उसके लिखे जाने के लगभग एक शताब्दी बाद पढ़ने वालों को इसमें उसी ताज़गी का एहसास होगा जो ताज़गी इसे पहली बार पढ़ने वालों ने महसूस की होगी। पढ़ाई के दौरान बार-बार यह सोचकर आश्चर्य होता है कि केवल 25 साल के एक युवक ने कितना अध्ययन कर रखा है। लोग अपना पूरा जीवन एक ही धर्म के शोध में लगा देते हैं, लेकिन इस युवक ने इतने कम समय में और सीमित संसाधनों के साथ सभी प्रमुख धर्मों का इतनी गहराई से और समीक्षात्मक अध्ययन कैसे कर लिया। साथ ही अतीत से वर्तमान तक संसार के हालात और उसके उतार चढ़ाव की बारीकियां भी उसके समक्ष रहीं।
एक सदी पहले मौलाना ने जिस ज़रूरत को देखते हुए यह किताब लिखी थी, वह आज भी अपनी पूर्ति की मांग कर रही है, बल्कि उसकी यह मांग पहले से अधिक तीव्र हो गई है। हैरानी और दुख की बात है कि इस किताब का प्रचार-प्रसार पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। अल-जिहाद फ़िल-इस्लाम के पहले प्रकाशन के 90 वर्षों बाद, 2017 में, इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ और अब, उसके भी 6 वर्ष बाद इसका हिंदी अनुवाद किया जा रहा है।
इस पुस्तक के संबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में मौलाना मौदूदी ने लिखा है, "मैंने इसके दूसरे संस्करण को इस विचार रोक रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून में जो परिवर्तन हो रहे थे उस पर एक टिप्पणी इस पुस्तक में जोड़ दी जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और मेरे लिए पढ़ना-लिखना बहुत मुश्किल हो गया।” तो द्वितीय विश्व युद्ध पर वह टिप्पणी, आज तक विद्वानों पर क़र्ज़ चली आ रही है, जिसे अविलम्ब चुका दिया जाना चाहिए। बल्कि हालात यह मांग करते हैं कि "सभ्यताओं के टकराव", "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" और उससे पहले संसाधनों की लूट और हथियारों की बिक्री की होड़ के परदे में, विश्व मंच पर जो कुछ हुआ, उस की व्यापक समीक्षा भी की जाए। विशेष रूप से युद्ध के उद्देश्य, युद्ध की सीमा और उसके तरीक़ों पर आज की "सभ्य" दुनिया की सोच और इसके अभ्यास का विश्लेषण किया जाए और उसे परिशिष्ट के रूप में इस किताब में शामिल किया जाए।
दूसरे, मौलाना मौदूदी ने हिंदू धर्म के संबंध में लिखा है: "मेरे सामने वेदों के अंग्रेजी अनुवाद हैं जो मिस्टर ग्रिफिथ की क़लम से निकले हैं। इसके साथ-साथ मैंने मैक्समूलर के अनुवादों का भी सामने रखा है। मुझे खेद है कि संस्कृत न जानने के कारण इन पुस्तकों को उनकी मूल भाषा में नहीं पढ़ सकता और यूरोपीय अनुवादकों का जो अनुभव हमें क़ुरआन के मामले में हुआ है, उस आधार पर हम हिंदू धर्म ग्रंथों के मामले में भी पश्चिमी अनुवादकों पर कुछ अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, मैं विद्वानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया वेदों के श्लोकों के अनुवाद पर मैंने जो कुछ लिखा है, उस पर आलोचनात्मक दृष्टि डालें। और यदि किसी अनुवाद में गलती है और मैंने इसके आधार पर गलत निष्कर्ष निकाला है, तो कृपया मुझे इसके बारे में सूचित करें।”
इस हिन्दी अनुवाद में मौलाना मरहूम की यह दूसरी ख़्वाहिश एक सदी बाद ही सही पूरी कर दी गई है। यह स्पष्ट रहे कि पाश्चात्य अनुवादकों ने वेदों तथा अन्य हिन्दू धर्मग्रन्थों के अनुवाद में कहीं डंडी मारने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। उपमाओं आदि के अनुवाद में कहीं-कहीं कुछ अन्तर तो है, मगर वह ऐसा नहीं है कि उससे भावार्थों में कोई अंतर पड़े, इसलिए उनसे ग़लत निष्कर्ष निकालने का कोई सवाल ही नहीं है।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया है और उन पर भाष्य भी लिखा है। इस पुस्तक के हिंदी के अनुवाद में दयानंद सरस्वती के अनुवादों का प्रयोग किया गया है। गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ‘सरल गीता’ से लिया गया है, जिसमें संस्कृत के श्लोकों के साथ-साथ उसका हिंदी अनुवाद और संक्षिप्त भाष्य भी है। इसी प्रकार, 'मनु स्मृति' के उद्धरण मनोज प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'मनु स्मृति', जिसमें संस्कृत छंदों के साथ सुरेंद्रनाथ सक्सेना द्वारा किया गया इंटरटेक्स्टुअल हिंदी अनुवाद शामिल है, से लिए गए हैं।
मौलाना द्वारा उद्धृत हिन्दू धर्मग्रन्थों के संदर्भ आरम्भ में अवश्य ही सही रहे होंगे, परन्तु बार-बार के लेखन (किताबत) में कई स्थान पर संख्यांकन के आगे-पीछे हो जाने के कारण वे ग़लत हो गये हैं। इस हिंदी अनुवाद में उन्हें सही कर दिया गया है। 'साम वेद' के जो जो संदर्भ मौलाना ने उसके अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर दर्ज किये हैं: जैसे (साम वेद: 3: 1: 5: 6-9), ऐसे संदर्भ बहुत खोजने पर भी न मिल सके। इन संदर्भों से पता चलता है कि पुस्तक को चार विभागों में विभाजित किया गया है, अर्थात, अध्याय, खंड, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, लेकिन इस समय उपलब्ध पुस्तकों में, इन सभी चारों विभागों को अपने स्थान पर छोड़ते हुए सामवेद के सभी मंत्रों को, जिनकी कुल संख्या 1875 है, एक क्रम संख्या दे दी गई है। उस क्रम संख्या के आधार पर उन्हें आसानी से खोजा जा सकता है, चाहे वह किसी अध्याय और खंड में हो, पूर्वार्चिक में से हो या उत्तरार्चिक में से। अब उपलब्ध पुस्तकों में पुराने चार-अवयवी संदर्भों के माध्यम से मंत्रों को खोजना असंभव नहीं तो अत्यधिक कठिन अवश्य हो गया है। इसलिए पूरा सामवेद पढ़ने के बाद युद्ध से संबंधित सभी मंत्रों का चयन कर लिया गया। लगभग वे सभी मंत्र मिल गये, जिन्हें मौलाना ने प्रस्तुत किया है, बल्कि उस विषय पर कुछ और मंत्र भी मिले, जिन्हें इस किताब में शामिल कर लिया गया है।
मौलाना ने बौद्ध धर्म की पुस्तक से केवल दो उद्धरण दिए हैं। बौद्ध धर्म की मूल पुस्तक (हिंदी अनुवाद सहित, पाली भाषा में) उप्लब्ध न होने के कारण इस किताब में मौलाना के उर्दू अनुवाद का ही हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है।
तोराह और इंजील के सभी अंश बाइबल के पुराने और नए नियम के हिंदी अनुवादों से लिए गए हैं। हिंदी में इन पुस्तकों का केवल एक ही अनुवाद उप्लब्ध है, जो भाषा और शैली से बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया प्रतीत होता है और उस पर किसी अनुवादक का नाम भी नहीं है। इसकी हिंदी आज की हिंदी से कुछ अलग है। उनमें से कई शब्द अब प्रचलन में नहीं रहे और कई शब्दों की वर्तनी भी बदल गई है।
इस पुस्तक के साथ एक परिशिष्ट की ज़रूरत आज भी बाक़ी है, जिसके लिए विद्वानों से संपर्क किया जा रहा है। आशा है कि जल्द ही एक व्यापक परिशिष्ट तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें मौलाना की इच्छा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध पर टिप्पणी भी शामिल होगी।
¬
पहला अध्याय
इस्लामी जिहाद की वास्तविकता
मानव जीवन का सम्मान:
पहला नियम जिस पर मानव सभ्यता की नींव टिकी है वह यह है कि मानव जीवन का सम्मान किया जाए। मनुष्य के नागरिक अधिकारों में पहला अधिकार जीने का अधिकार है और उसके नागरिक दायित्वों में पहला दायित्व जीने देने का दायित्व है। मानव जान के सम्मान का यह नैतिक सिद्धांत दुनिया के सभी धर्मविधानों और सभ्य क़ानूनों में ज़रूर मौजूद है। जिस क़ानून और धर्म में इसे मान्यता नहीं दी गई है, वह सभ्य लोगों का धर्म और क़ानून नहीं बन सकता है और न ही उसके अधीन रह कर कोई भी मानव समुदाय शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, और न ही उसका कोई विकास हो सकता है। हर व्यक्ति की समझ सकता है कि अगर मानव जीवन का कोई मूल्य न हो, उसका कोई सम्मान न हो, उसकी रक्षा का कोई प्रावधान न हो तो चार लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, आपस में कैसे बातचीत कर सकते हैं? उनके बीच व्यापार-विनिमय कैसे हो सकता है। उन्हें वह शांति और सद्भाव, वह संतुष्टि और वह सहजता कैसे मिल सकती है, जिसकी मनुष्य को व्यापार-विनिमय, उद्योग-धंधे, खेती-वाड़ी करने, धन कमाने, घर बनाने, यात्रा करने और सभ्य जीवन की दूसरी गतिविधियों के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर ज़रूरत की परवाह किये बिना शुद्ध मानवता की दृष्टि से देखा जाय तो अपने किसी स्वार्थ के लिये या किसी निजी शत्रुता के लिये अपने एक भाई की हत्या करना सबसे घोर निर्दयता और अधर्म है, ऐसा जघन्य अपराध करने के बाद मनुष्य में नैतिक उत्थान तो परे, उसका मनुष्यता के स्तर पर टिके रहना भी असम्भव है।
दुनिया के राजनीतिक क़ानून तो केवल दंड के भय और बलप्रयोग के आधार पर ही मानव जीवन के लिए यह सम्मान स्थापित करते हैं, लेकिन एक सच्चे धर्म का काम दिलों में इसका सही मूल्य पैदा करना है, ताकि जहां मानव दंड का कोई डर न रहे और जहां रोकने के लिए कोई मानव पुलिस न हो, वहां भी आदम की संतान एक दूसरे के अन्यायपूर्ण रक्तपात से बचे रहें। इस दृष्टि से इस्लाम में मानव जान के सम्मान की जैसी सही और प्रभावी शिक्षा दी गई है, वह किसी अन्य धर्म में मिलना मुश्किल है। पवित्र क़ुरआन में विभिन्न स्थानों पर इस शिक्षा को दिलों में बिठाने का प्रयास किया गया है। सूरह मायदा में आदम के दो पुत्रों की कहानी सुनाते हुए, जिनमें से एक ने अन्यायपूर्ण ढंग से दूसरे को मार डाला था, कहा:
مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. (المائدہ : ۳۲)
“इसीलिए हमने इसराईल की सन्तान को यह लिख कर दे दिया कि जो कोई किसी की जान ले, बिना इस के कि उस ने किसी की जान ली हो, या ज़मीन में फ़साद किया हो, तो मानो उसने सारे इन्सानों का ख़ून बहाया है। और जिसने किसी की जान बचाई, मानो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। हमारे रसूल इन लोगों के पास स्पष्ट मार्गदर्शन लेकर आये, फिर भी उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो धरती में अपनी सीमा से आगे बढ़ जाते हैं।” (अल-मायदा: 32)
एक दूसरी जगह अल्लाह अपने नेक बन्दों के गुण बताते हुए कहता है :
وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًۭا .(الفرقان: ۶۸)
“वे उस जान को, जिसे अल्लाह ने सम्मानित ठहराया है, बिना हक़ के नहीं मारते और न ही वे व्यभिचार करते हैं, और जो कोई भी ऐसा करेगा, वह अपने कर्मों के लिए दंडित किया जाएगा।” (अल-फ़ुर्क़ान : 68)
एक अन्य स्थान पर कहा जाता हैं:
قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًۭٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًۭا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍۢ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ (الانعام : ۱۵۱)
“ऐ मुहम्मद कहो कि आओ! मैं तुमको बताता हूं कि अल्लाह ने तुम पर क्या-क्या प्रतिबंध लगाए हैं। यह तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम किसी को अल्लाह के साथ साझी न बनाओ, अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो और अपने बच्चों को ग़रीबी और तंगी की वजह से कत्ल न करो, हम जहां से तुम्हें रोजी देते हैं, उन्हें भी देंगे, दुष्कर्मों के क़रीब भी न जाओ, चाहे वे छिपे हों या खुले, किसी ऐसी जान को, जिसे अल्लाह ने सम्मानित ठहराया हो, कत्ल न करो, सिवाय इसके कि ऐसा करना सत्य को वोंछित हो, अल्लाह ने इन बातों पर बल दिया है, शायद कि तुममें कुछ समझ आ जाए।” (अल-अनआम: 151)
इस शिक्षा का प्राथमिक सम्बोघन उन लोगों की ओर था, जिनके लिए मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं था, और जो अपने निजी लाभ के लिए अपनी संतान तक को मार डालते थे। इसलिए इस्लाम के आवाहक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) हमेशा उनके व्यवहार में सुधार के लिए ख़ुद भी मानव जान का सम्मान करने का उपदेश देते रहते थे, और यह उपदेश हमेशा बहुत प्रभावी होता था। हदीसों में इस तरह की कई बातें हैं जिनमें निर्दोष लोगों का ख़ून बहाना सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है। उदाहरण के लिए, हम यहां कुछ हदीसों का हवाला देते हैं।
अनस बिन मलिक से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा:
“बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ भागीदारों को जोड़ना और किसी को जान से मारना और माता-पिता की अवज्ञा करना और झूठ बोलना है।”
हज़रत इब्ने उमर से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा:
“ईमानवाला अपने दीन (धर्म) की सीमा में तब तक बराबर रहता है जब तक वह कोई वर्जित ख़ून नहीं बहाता है।”
“क़ियामत के दिन बन्दे से सब से पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वह नमाज़ है, और सबसे पहली चीज़ जिसका फ़ैसला लोगों के बीच किया जाएगा वह ख़ून के दावे हैं।”
एक बार एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की सेवा में आया और पूछा, “सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है?”
आपने कहा: “यह कि तुम किसी को अल्लाह के समकक्ष ठहराओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया।”
फिर उसने पूछा कि उसके बाद कौन सा गुनाह बड़ा है?
आपने उत्तर दिया: “यह कि तुम अपने बच्चे को यह सोचकर मार डालो कि वह तुम्हारा भोजन साझा करेगा।”
उसने कहा कि उसके बाद कौन सा गुनाह है?
आपने कहा: “यह कि तुम अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ व्यभिचार करो।”
दुनिया पर इस्लामी शिक्षा का नैतिक प्रभाव
मानव जान के सम्मान की यह शिक्षा किसी दार्शनिक या नैतिकता के किसी शिक्षक के प्रयत्नों का परिणाम नहीं थी कि इसका प्रभाव केवल किताबों और मदरसों तक ही सीमित रहता, बल्कि वास्तव में यह अल्लाह और उसके रसूल की शिक्षा थी जिसका एक-एक शब्द हर मुसलमान के ईमान का अंश था। जिसका अनुपालन, जिसका प्रसार और जिसे स्थापित करना हर उस व्यक्ति पर फ़र्ज़ है जो इस्लाम का मानने वाला हो। तो एक चौथाई सदी की छोटी अवधि में, इस शिक्षा की बदौलत अरबों जैसे रक्तपिपासु क़ौम में मानव जान के सम्मान और शांतिप्रियता की ऐसी भावना पैदा हो गई कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की भविष्यवाणी के अनुसार, एक महिला ‘क़ादसिया’ से ‘सनआ’ तक अकेले यात्रा करती थी और कोई उसकी जान और संपत्ति पर हमला नहीं करता था। हालांकि यह वही देश था जहां पच्चीस साल पहले बड़े-बड़े कारवां भी बिना डरे नहीं गुज़र पाते थे। फिर, जब आधी से अधिक सभ्य दुनिया इस्लाम के शासन में आ गई और इस्लाम का नैतिक प्रभाव दुनिया के कोने-कोने में फैल गया, तो इस्लामी शिक्षा ने, मनुष्य के कई ग़लत कामों और त्रुटियों की तरह, मानव जान की उस मूल्यहीनता को भी ख़त्म कर दिया, जो विश्व भर में फैली हुई थी। आज दुनिया के सभ्य क़ानूनों में मानव जान को सम्मान का जो दर्जा मिला है, वह उस क्रांति के अद्भुत परिणामों में से एक है, जो इस्लामी शिक्षा के कारण दुनिया के नैतिक वातावरण में आई। अन्यथा, जिस अन्धकार युग में इस शिक्षा का अवतरण हुआ, उसमें मानव जीवन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं था।
दुनिया ने इस सिलसिले में ख़ून के प्यासे अरबों का नाम सुना है, लेकिन उस दौर में उन देशों की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो सभ्यता, शालीनता, ज्ञान और विवेक के केंद्र बने हुए थे। रोम के कोलोसियम की कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसमें हज़ारों लोग ग्लैडिएटरी (तलवारबाज़ी) के कारनामों और रोमन रईसों के तमाशा देखने के शौक़ की भेंट चढ़ जाते थे। मेहमानों और दोस्तों के मनोरंजन के लिए, ग़ुलामों को जंगली जानवरों से फड़वा देना, या उन्हें जानवरों की तरह चीर डालना या उन्हें जलते हुए देखना यूरोप और एशिया के कई देशों में कोई बुरी बात नहीं थी। क़ैदियों और ग़ुलामों को तरह-तरह से यातनाएं देकर मार डालना उस युग का सामान्य अभ्यास था। अज्ञानी और रक्तपिपासु रईसों से लेकर यूनान और रोम के महान शासकों और दार्शनिकों तक, निर्दोष मानव जीवन की हत्या के कई बर्बर रूपों की अनुमति थी। अरस्तू और प्लेटो जैसे नैतिकता के गुरुओं को भी माताओं को अपने शरीर के एक अंग (अर्थात् भ्रूण) को हटाने का अधिकार देने में कुछ भी ग़लत नहीं दिखाई देता था। इसलिए ग्रीस और रोम में गर्भपात अवैध नहीं था। पिता को अपनी संतान की हत्या का पूरा अधिकार था, और रोमन विधिनिर्माताओं को अपने क़ानून की विशेषता पर गर्व था कि उसमें संतान पर पिता के अधिकार इतने असीमित हैं। स्टोइक्स के अनुसार मनुष्य का स्वयं को मार डालना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि यह एक सम्माननीय कार्य था। लोग सम्मेलन आयोजित कर के आत्महत्याएं करते थे। हद तो यह है कि प्लेटो जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी इसे कोई बड़ा गुनाह नहीं मानता था। एक पति के लिए अपनी पत्नी की हत्या बिलकुल ऐसी थी, जैसे कोई अपने एक पालतू जानवर को मार डाले, इसलिए ग्रीक क़ानून में इसके लिए कोई सज़ा नहीं थी।
जीव रक्षा का केंद्र हमारा देश भारत इन सभी से बढ़ा हुआ था, यहां एक महिला को एक पुरुष की चिता पर ज़िंदा जलाना एक वैध, बल्कि पावन कार्य समझा जाता था और धार्मिक रूप से स्वीकृत था। (कहने वाला कह सकता है कि औरतें अपने पतियों की चिता में जलाई नहीं जाती थीं, बल्कि स्वेच्छा से जलती थीं। लेकिन सच तो यह है कि समाज का तरह-तरह का दबाव ही उन्हें उस भयानक आत्महत्या के लिए मजबूर करता था।) एक शूद्र के जीवन का कोई मूल्य न था। केवल इस आधार पर कि वह बेचारा ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ था, उसका ख़ून एक ब्राह्मण के लिए वैध था। एक शूद्र के लिए वेद की वाणी सुनना इतना बड़ा गुनाह था कि उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालकर उसे मार डालना न केवल अनुज्ञेय था बल्कि अनिदार्य भी था। “जल-प्रदाह” की प्रथा आम थी, जिसके अनुसार कई माता-पिता अपनी पहली संतान को गंगा नदी की भेंट चढ़ा देते थे, और इस क्रूरता को अपने लिए सौभाग्य समझते थे।
ऐसे अँधेरे युग में इस्लाम ने आवाज़ उठाई कि:
“मानव जीवन को अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है, इस की हत्या मत करो, सिवाय इसके कि सत्य उसकी हत्या की मांग करता हो।” इस आवाज़ में एक शक्ति थी और शक्ति के साथ वह, “अहिंसा परमो धर्म:” की आवाज़ की तरह, यह बुद्धि-विवेक और प्रकृति के प्रतिकूल भी न थी। इसलिए वह दुनिया के कोने-कोने में पहुंची और लोगों को अपने जीवन के सही मूल्य से अवगत कराया। किसी राष्ट्र या देश ने इस्लाम के दायरे में आना स्वीकार किया हो या न किया हो, उसका नैतिक जीवन किसी हद तक इस आवाज़ के प्रभाव को स्वीकार किए बिना नहीं रहा। सामूहिक इतिहास का कोई भी निष्पक्ष विद्वान इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि संसार के नैतिक नियमों में मानव जीवन की पवित्रता को स्थापित करने का जितना श्रेय इस आवाज़ को प्राप्त है, उतना “पहाड़ी का धर्मोपदेश” या “अहिंसा परमो धर्म:” की आवाज़ को नहीं है।
न्याय के आधार पर हत्या
लेकिन ध्यान से देखो, केवल यही नहीं कहा गया, “मानव जीवन को अल्लाह सर्वशक्तिमान द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है, इस की हत्या मत करो”, बल्कि इसके साथ यह भी कहा, सिवाय इसके कि सत्य उसकी हत्या की मांग करता हो।”
केवल यही नहीं कहा गया, “जिसने किसी की आदमी की जान ली है, तो मानो उसने सारे इन्सानों का ख़ून बहाया है।” बल्कि इसके साथ यह अपवाद भी रखा गया, “बिना इस के कि उस ने किसी की जान ली हो, या ज़मीन में बिगाड़ फैलाया हो।”
ऐसा नहीं कहा गय कि किसी भी हालत में किसी की जान नहीं लो। अगर ऐसा कहा जाता तो यह शिक्षा का दोष होता। कोई न्याय नहीं होता, बल्कि अत्याचार होता। संसार की वास्तविक ज़रूरत यह नहीं थी कि मनुष्य को क़ानून के शिकंजे से खुली छूट दे दी जाए, वह चाहे जितना उत्पात मचाए, जितनी चाहे अशांति फैलाए, जितना चाहे अत्याचार करे, उसका जीवन हर हाल में आदरणीय बना रहेगा, बल्कि असल ज़रूरत थी दुनिया में शांति स्थापित करने की, उत्पात और अशांति को मिटाने की और ऐसा क़ानून बनाने की, जिसके अनुसार हर व्यक्ति अपनी सीमा में स्वतंत्र हो और कोई व्यक्ति अपनी निश्चित सीमा का उल्लंघन करके दूसरों की भौतिक या आध्यात्मिक शांति को भंग न करे। इस प्रयोजन के लिए मात्र, “मानव जान की हत्या न करो” का समर्थन ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि, “सिवाय इसके कि सत्य उसकी हत्या की मांग करता हो।” के सुरक्षात्मक बल की भी ज़रूरत थी, अन्यथा शांति के बजाय अशांति फैल जाती।
दुनिया का कोई भी क़ानून जो ‘कर्म के अनुरूप फल’ के सिद्धांत से ख़ाली हो, सफलता तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य स्वभाव से इतना आज्ञाकारी नहीं है कि जो आज्ञा दी जाए उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर ले और निषिद्ध को स्वेच्छा से त्याग दे। अगर ऐसा होता तो दुनिया में उत्पात और अशांति नाम मात्र को भी नहीं होती। मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई के साथ-साथ बुराई और आज्ञाकारिता के साथ-साथ अवज्ञा भी है। इसलिए, उसके विद्रोही स्वभाव को आज्ञाकारिता पर मजबूर करने के लिए ऐसे क़ानून की ज़रूरत है, जिसमें आदेश देने के साथ-साथ यह भी बताया गया हो कि पालन न करने पर दण्ड क्या है। निषेधाज्ञा के साथ-साथ यह भी हो कि अगर वर्जित कर्म को न छोड़ा गया तो क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा।
केवल यह कहना पर्याप्त नहीं हो सकता कि “धरती पर, इसके सुधार के बाद बिगाड़ न फैलाओ” या “उस जान की हत्या मत मारो, जिसे अल्लाह ने हराम किया है”, जब तक कि यह भी न बता दिया जाए कि अगर इस महान अपराध से किसी ने परहेज़ नहीं किया और बिगाड़ फैलाया और हत्या और ख़ून-ख़राबा, किया तो उसके लिए क्या सज़ा होगी।
मानव शिक्षा में ऐसी त्रुटि रह जाना संभव है, लेकिन ईश्वरीय विधान इतना त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता। उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मानव जान का सम्मान तभी तक है जब तक उस पर “हक़” स्थापित नहीं हो जाता। उसे जीवन का अधिकार उसकी वैध सीमा के भीतर ही दिया जा सकता है, लेकिन जब वह उन सीमाओं का उल्लंघन करता है और उत्पात मचाता है, दुराचार करता है, दूसरों के जीवन पर अन्यायपूर्ण हमले करता है, तो वह स्वतः ही जीवन का अधिकार खो देता है। उसके ख़ून की पवित्रता समाप्त हो जाती है, और फिर उसकी मौत इंसानियत की जान बन जाती है। अत: कहा गया: “वध करना बहुत बुरा है, लेकिन उस से ज़्यादा बुरी चीज़ उत्पात और अशांति है।” जब कोई व्यक्ति इस जघन्य अपराध का दोषी हो तो उसकी बड़ी बुराई का अंत कर देना ही बेहतर है। इसी तरह जो व्यक्ति अन्यायपूर्ण ढंग से दूसरे की जान ले ले उस के लिए भी आदेश सुनाया गया: “तुम्हें आदेश दिया गया है कि जिसकी हत्या की गई हो उसकी मौत का क़िसास (ख़ून का बदला) लिया जाए।”
इसके साथ ही ऊँच-नीच के उस भेद के भी मिटा दिया गया, जो दिग्भ्रमित राष्ट्रों ने स्थापित किया था। अत: कहा गया, “और हम ने यह आदेश दिया कि एक जान के बदले एक जान”, यह नहीं हो सकता कि धनवान निर्धन को मारें या आज़ाद व्यक्ति दास को मारे, तो उसे छोड़ दिया जाए, बल्कि मनुष्य होने की दृष्टि से सभी समान हैं। जीवन के बदले जीवन ही लिया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या ग़रीब। फिर इस विचार से कि किसी को इस अपरिहार्य रक्तपात में झिझक न हो, कहा गया: “और ऐ बुद्धिमान व्यक्ति! इस क़िसास (ख़ून के बदले) को मृत्यु मत समझो, बल्कि यह वास्तव में समाज का जीवन है, जो उसके शरीर से एक घातक फोड़े को काटकर प्राप्त किया जाता है। ‘क़िसास में जीवन है’ के दर्शन की अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने एक मौक़े पर बड़ी अच्छी व्याख्या की है। कहा, “अपने भाई की मदद करो, चाहे वह अत्याचारी हो या पीड़ित” सुनने वालों को हैरत हुई कि पीड़ितों की मदद तो ठीक है, लेकिन अत्याचारी की कैसी मदद? पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा, “इस तरह से कि तुम उसका हाथ पकड़ लो और उसे अत्याचार से रोको।” इसलिए वास्तव में अत्याचारी की क्रूरता को रोकने के लिए उसके साथ जो भी कठोरता की जाती है वह कठोरता नहीं बल्कि सज्जनता होती है और स्वयं अत्याचारी की भी सहायता होती है। इसी लिए इस्लाम में अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमाओं को स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है और इसे दया और वरदान बताया गया है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कहा कि अल्लाह की सीमाओं में से एक को स्थापित करने की बरकत 40 दिनों की बारिश से अधिक है। वर्षा की बरकत यह है कि इससे भूमि सिंचित होती है, फसलें अच्छी होती हैं, समृद्धि बढ़ती है। लेकिन सीमाओं की स्थापना की बरकत इससे कहीं अधिक है कि इस से अत्याचार, बिगाड़ और अशांति की जड़ कटती है, अल्लाह की सृष्टि को शांति से रहने का आशीर्वाद मिलता है, और शांति की स्थापना से समृद्धि आती है, जो सभ्यता का जीवन है, और प्रगति की आत्मा है।
न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण हत्या के बीच अंतर
हक़ के बिना क़त्ल करने की इतनी सख़्त मनाही और हक़ के साथ क़त्ल पर इतना ज़ोर देकर, अल्लाह की शरीयत (विधिविधान) ने हमें न्याय और संतुलन के सीधे रास्ते की ओर निर्देशित किया है। एक ओर अतिवादी और अत्याचारी समूह है जो मानव जीवन को कोई महत्व नहीं देता और अपनी मनेच्छाओं पर उसे बलि चढ़ा देना उचित समझता है। दूसरी ओर, वह भ्रमित और संकीर्ण सोच वाला समूह है जो रक्त के सम्मान और उसकी शाश्वत पवित्रता का पक्षधर है और किसी भी परिस्थिति में इसे बहाने को जायज़ नहीं मानता है।
इस्लामी शरीयत ने इन दोनों ग़लत विचारों को रद्द कर दिया और कहा कि मानव जान की पवित्रता न तो काबा या मां-बहन की पवित्रता की तरह शाश्वत है, कि किसी भी हाल में उसकी हत्या जायज़ ही न हो, और न ही इसका मूल्य इतना कम है कि मनेच्छाओं की संतुष्टि के लिए उसे मारने की अनुमति हो। एक ओर, उसने बताया कि मानव जीवन इस लिए नहीं है मनोरंजन के लिए उसे मार कर तड़पता हुआ देखा जाए, उसे जलाकर या प्रताड़ित कर के आनंद लिया जाए, या उसे व्यक्तिगत हितों के रास्ते में बाधा समझकर मौत के घाट उतार दिया जाए, या उसे अंधविश्वास और ग़लत कर्मकांड की वेदी पर भेंट चढ़ा दिया जाए। इस तरह के नापाक उद्देश्यों के लिए इसका ख़ून बहाना निश्चित रूप से निषिद्ध और घोर अपराध है। दूसरी ओर उसने यह भी बताया कि एक चीज़ इंसान की जान से भी ज़्यादा क़ीमती है और वह है “सत्य”। वह जब उसके ख़ून की मांग करे, तो उसे बहाना न केवल जायज़ है बल्कि अनिवार्य है, और उसे नहीं बहाना अपराध है। इंसान जब तक सत्य का सम्मान करता है, तब तक उसका ख़ून सम्मान येग्य रहता है, लेकिन जब वह उद्दंडता कर के सत्य पर हमला कर देता है, तो वह अपने ख़ून का मूल्य खो देता है। फिर उसके ख़ून का मूल्य पानी जितना भी नहीं होता है।
अपरिहार्य रक्तपात
यह न्यायाधारित हत्या, यद्यपि देखने में अन्यायपूर्ण हत्या के समान रक्तपात है, लेकिन वास्तव में यह अपरिहार्य रक्तपात है जिससे किसी हाल में छुटकारा नहीं। इसके बिना विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है, न ही बुराई और बिगाड़ की जड़ काटी जा सकती है। न भले लोगों को दुष्टों की दुष्टता से मुक्ति मिल सकती है, न ही लोगों को उनका अधिकार मिल सकता है, और न ही ईमानदारों को विश्वास और विवेक की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। न उत्पातियों को उनकी वैध सीमाओं के भीतर प्रतिबंधित किया जा सकता है, और न ही अल्लाह की सृष्टि को भौतिक और आध्यात्मिक शांति मिल सकती है। अगर इस्लाम पर इस तरह के रक्तपात का आरोप लगाया जाता है, तो उसे इस आरोप को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा कौन है जिसका दामन इस अपरिहार्य रक्तपात के छींटों से लाल नहीं है?
बौद्ध धर्म की अहिंसा इसे नाजायज़ मानती है, लेकिन उसे भी भिक्षुओं और गृहस्थों के बीच अंतर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंत में, एक छोटे समूह के लिए निर्वाण को आरक्षित करने के बाद, उसने बाक़ी दुनिया को कुछ नैतिक निर्देश देकर गृहस्थ धर्म को अपनाने के लिए छोड़ दिया, जिसमें राजनीति, दंड और युद्ध सभी हैं।
इसी तरह ईसाइयत भी युद्ध के पूर्ण निषेध के बावजूद युद्ध करने पर मजबूर हुई और जब रोमन साम्राज्य के अत्याचारों को सहन करना उसके लिए असंभव हो गया, तो उसने अंततः साम्राज्य को ही अपने क़ब्ज़े में ले लिया और ऐसा युद्ध छेड़ दिया जो अनिवार्य रक्तपात की सीमा से बहुत आगे निकल गया।
हिन्दू धर्म में भी बाद के दार्शनिकों ने “अहिंसा परमो धर्म:” का सिद्धांत प्रस्तावित किया और जीव-हत्या को पाप घोषित किया, लेकिन उसी काल के विधिनिर्माता ‘मनु’ से पूछा गया था कि “अगर कोई हमारी महिलाओं पर हाथ डालता है, या हमारी संपत्ति चुराता है, और हमारे धर्म का अपमान करता है, तो हमें क्या करना चाहिए?” तो उसने उत्तर दिया, “ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अवश्य ही मार देना चाहिए, चाहे वह गुरू हो या विद्वान ब्राह्मण, बूढ़ा हो या जवान।”
यहां धर्मों की तुलना करके इस अपरिहार्य रक्तपात की ज़रूरत को सिद्ध करने का अवसर नहीं है। धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन एक अलग विषय है जो अपने समय पर आएगा और तब यह सिद्ध हो जाएगा कि जो धर्म युद्ध को अशुभ मानते हैं वे भी व्यावहारिक जगत् में प्रवेश करने के बाद इस अवश्यंभावी चीज़ से बचने में असफल रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि नैतिकता के प्रदर्शन के लिए कोई समूह चाहे कितने भी उच्च काल्पनिक दर्शन तक पहुंच जाए, लेकिन अभ्यास की दुनिया में आकर उसे व्यावहारिक परिस्थितियों के माध्यम से दुनिया की सभी समस्याओं को हल करना है पड़ता है और यह दुनिया ख़ुद उसे मजबूर कर देती है कि वह इसकी वास्तविकताओं का व्यावहारिक उपायों के साथ सामना करे। क़ुरआन को उतारने वाले के लिए मुश्किल नहीं था कि वह मानव जीवन के सम्मान के लिए वैसे ही काल्पनिक आनंद देने वाले सिद्धांत प्रस्तुत करता, जैसे अहिंसा की धारणा में पाए जाते हैं। निश्चित रूप से वह उन्हें अपने चमत्कारी शब्दों में प्रस्तुत कर के दुनिया को अचंभित कर सकता था। लेकिन जगत के निर्माता का यह उद्देश्य नहीं था, बल्कि वह अपने बन्दों के लिए एक सही और स्पष्ट मैनुअल पेश करना चाहता था, जिस का पालन कर वे अपनी दुनिया और परलोक को ठीक कर सकें।
यह अल्लाह का ज्ञान और उसकी तत्वदर्शिता थी कि उसने हत्या को वर्जित ठहराने की शिक्षा के साथ क़िसास के क़ानून को भी निर्धारित किया और इस प्रकार उस बल के प्रयोग को आवश्यक बना दिया जिसका प्रयोग मानव जान की सुरक्षा के लिए अनिवार्य था ।
सामुदायिक बिगाड़
क़िसास का यह क़ानून जिस तरह व्यक्तियों के लिए है, उसी तरह समुदायों के लिए भी है। जैसे व्यक्ति उद्दंड होते हैं, वैसे ही समुदाय और राष्ट्र भी उद्दंड होते हैं। जैसे व्यक्ति लोभ में पड़कर मर्यादा लांघ जाते हैं, वैसे ही समुदायों और राष्ट्रों में भी यह नैतिक रोग पैदा हो जाता है। इसलिए, जिस तरह व्यक्तियों को नियंत्रण में रखने और उद्दंडता को रोकने के लिए रक्तपात आवश्यक है, समुदायों और राष्ट्रों के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए युद्ध अपरिहार्य हो जाता है।
प्रकृति की दृष्टि से व्यक्तिगत और सामुदायिक फ़ित्ना (बिगाड़) में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्वरूप में बहुत अंतर है, व्यक्ति का फ़ित्ना एक सीमित दायरे तक ही रहता है, लोगों का एक छोटा समूह उससे आहत होता है, और गज़ भर ज़मीन को रंगीन करके उसका अंत किया जा सकता है, लेकिन समुदायों का फ़ित्ना एक असीमित मुसीबत होता है, जिससे अनगिनत लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, पूरे पूरे राष्ट्रों का जीवन संकट में आ जाता है, और सभ्यता की पूरी व्यवस्था में, एक हलचल मच जाती है, और उसका अंत ख़ून की नदियां बहाए बिना नहीं किया जा सकता है।
जब समुदायों द्वारा उत्पात मचाया जाता है, तो कोई एक बिगाड़ पैदा नहीं होता है, विभिन्न शैतानी ताक़तें उनके तूफ़ानों में सर उठाती हैं और हज़ारों तरह के बिगाड़ उनके कारण उठ खड़े होते हैं। कुछ जो धन के लोभी होते हैं, वे ग़रीब क़ौमों पर डाके डालते हैं, उनके व्यापार पर क़ब्ज़ा करते हैं, उनके उद्योगों को नष्ट कर देते हैं, उनकी मेहनत की कमाई को तरह-तरह की तरकीबों से लूट कर अपनी तिजोरी भरते हैं। उनमें से कुछ मनेच्छाओं के ग़ुलाम होते हैं, तो वे अपने जैसे इन्सानों के ख़ुदा बन जाते हैं, कमज़ोरों के अधिकारों को अपनी इच्छाओं पर क़ुरबान करते हैं, और न्याय को मिटा कर अत्याचार और अन्याय स्थापित करते हैं। भले और सज्जन लेगों को दबा कर मूर्खों और कमीनों को सिर चढ़ाते हैं। उनके नापाक प्रभाव से राष्ट्रों की नैतिकता समाप्त हो जाती है, सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, और उनके स्थान पर धोखा, विश्वासघात, नैतिक पतन, व्यभिचार, क्रूरता, अन्याय, अत्याचार और अनगिनत दूसरे नैतिक दोष पैदा हो जाते हैं। फिर उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर साम्राज्यविस्तार का भूत सवार होता है, तो वे असहाय और कमज़ोर राष्ट्रों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं, अल्लाह के निरपराध बन्दों का ख़ून बहाते हैं, ताकि वे धरती पर सत्ता की अपनी इच्छा पूरी कर सकें। बिगाड़ फैलाते हैं और आज़ाद आदमियों को उस ग़ुलामी में जकड़ देते हैं जो सभी नैतिक बुराइयों की जड़ है। इन शैतानी हरकतों के साथ बलात् धर्म परिवर्तन भी शामिल हो जाता है जब कुछ दमनकारी समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का उपयोग करने लगते हैं और अल्लाह के बन्दों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित कर देते हैं। जब वे इस वजह से दूसरों पर अत्याचार करते हैं, कि वे उनकी पसंद के धर्म के बजाय किसी और धर्म का पालन क्यों करते हैं, तो यह मुसीबत और गंभीर हो जाती है।
युद्ध : एक सामाजिक और नैतिक दायित्व
ऐसी में युद्ध जायज़ ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। उस समय मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि उन ज़ालिमों के ख़ून से धरती को लाल कर दिया जाए और उन उत्पातियों अत्याचारियों की बुराई से अल्लाह के शोषित और लाचार बन्दों को छुटकारा दिलाया जाए। वे लोग वास्तव में मनुष्य नहीं होते जो मानवीय सहानुभूति के पात्र हों, बल्कि वे मानव वेश में शैतान और मानवता के असली शत्रु होते हैं, जिनके साथ वास्तविक सहानुभूति यही है कि उनकी बुराई को मिटा दिया जाए। वे स्वयं अपने कर्मों के कारण जीवन का अधिकार खो देते हैं। उन्हें और उन लोगों को भी, जो उनकी बुराई को जारी रखने में उनकी मदद करते हैं, दुनिया में जीवित रहने का अधिकार बाक़ी नहीं रहता, वे वास्तव में मानवता के शरीर के उस अंग के समान हैं, जिसमें ज़हरीला और दूषित मवाद भर गया हो, जिसको अगर छोड़ दिया गया तो पूरे शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि उस अंग को काट फेंका जाए।
यह संभव है कि दुनिया में एक कल्पनाशील नैतिक शिक्षक ऐसा भी हो, जिसके अनुसार ऐसे अत्याचारियों की हत्या भी पाप हो, और जिसकी कायर आत्मा उस ख़ून के विचार से कांप उठती हो जो उनकी बुराई को दूर करने के लिए बहता है, लेकिन ऐसा शिक्षक दुनिया को सुधार नहीं सकता। वह जंगलों और पर्वतों पर जाकर तपस्या से अपनी आत्मा को तृप्त तो कर सकता है, पर उसकी शिक्षा संसार को बुराई से मुक्त करने और क्रूरता और विद्रोह से सुरक्षित रखने में कभी सफल नहीं हो सकती। वह निश्चित रूप से आत्म-विनाशकारी लोगों का एक ऐसा समूह प्रदान कर सकता है जो उत्पीड़ितों के साथ अत्याचार सहने में सहभागी हो जाए, मगर उत्साही ओर जियाले लोगों का एक समूह तैयार करना उसके वश की बात नहीं, जो अत्याचार को मिटा कर न्याय की स्थापना कर दे और अल्लाह की सृष्टि के लिए शांति से रहने और मानवता के उच्चतम लक्ष्यों तक पहुँचने के साधन उपलब्ध करा दे।
व्यावहारिक नैतिकता, जिसका उद्देश्य सभ्यता की एक उचित प्रणाली स्थापित करना है, वास्तव में एक दूसरा ही दर्शन है, जिसमें काल्पनिक आनंद का साधन ठूंडना व्यर्थ है। जिस प्रकार चिकित्सा का उद्देश्य स्वाद उपलब्ध कराना नहीं है, शरीर का सुधार है, चाहे कड़वी औषधि से हो या मीठी से। उसी प्रकार नैतिकता का लक्ष्य मन और आंखों को आनन्द पहुंचाना नहीं है, बल्कि संसार का सुधार है, चाहे वह कठोरता से हो या नर्मी से। कोई सच्चा समाज सुधारक तलवार और क़लम में से केवल एक को अपनाकर उसके माध्यम से सुधार करने की शपथ नहीं ले सकता। उसे अपने काम को पूरा करने के लिए दोनों की समान रूप से ज़रूरत होती है। जब तक हिंसक समुदायों को नैतिकता और मानवता की मर्यादाओं में रहने के लिए मजबूर करने में उपदेश कारगर हो सकते हैं, तब तक उनके ख़िलाफ़ तलवार चलाना न केवल नाजायज़ है बल्कि वर्जित भी है। मगर जब किसी समुदाय की दुष्टता और आंतरिक बुराई इस हद को पार कर चुकी हो कि उसे उपदेश और प्रेरणा देकर सही रास्ते पर लाया जा सके। जब उसे दूसरों की गरिमा और सम्मान पर हमला करने से और लोगों के नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन पर प्रहार करने से रोकने का कोई उपाय युद्ध के सिवा न रह गया हो, तो फिर यह मानवता के हर सच्चे शुभचिंतक का पहला दायित्व हो जाता है कि वह इसके ख़िलाफ़ तलवार उठाए और तब तक चैन न ले जब तक कि अल्लाह की सृष्टि को उनके खोए हुए अधिकार वापस नहीं मिल जाते।
युद्ध का औचित्य
युद्ध की समीचीनता और ज़रूरत को अल्लाह, तत्वदर्शी और सर्वज्ञ ने अपने कथन में प्रकट किया है:
وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌۭ وَصَلَوَٰتٌۭ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ۗ.(الحج: ۴۰)
“और अगर अल्लाह कुछ लोगों की, कुछ लोगों द्वारा, प्रतिरक्षा न कराता तो आश्रम, गिरजाघर, यहूदियों के धर्म स्थल और मस्जिदें, जिनमें अल्लाह का नाम अधिक लिया जाता है, सब ध्वस्त कर दिये जाते।” (अल-हज: 40).
इस पवित्र आयत में केवल मुसलमानों की मस्जिदों का उल्लेख ही नहीं किया गया है, बल्कि अन्य धर्मों के पवित्र स्थलों और ऐसे व्यापक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत हर धर्म के पूजास्थल आते हैं, का भी उल्लेख किया है। इससे उद्देश्य यह संदेश देना है कि अगर अल्लाह न्यायप्रिय लोगों के माध्यम से ज़ालिमों को ख़त्म न करता रहता, तो इतना अधिक उत्पात मचता कि पूजास्थल भी विनाश से नहीं बच पाते, जिससे किसी को नुक़सान होने का डर नहीं होता। इसके साथ यह भी बता दिया कि बिगाड़ का सबसे घिनौना रूप यह है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के धर्मस्थलों को भी शत्रुता से नष्ट कर दे। फिर बड़े ही ओजस्वी अंदाज़ में अपनी यह मंशा भी ज़ाहिर कर दी कि जब कोई समूह इस तरह का उत्पात मचाता है तो हम दूसरे समूह के ज़रिये उसके उत्पात का दमन ज़रूरी समझते हैं।
युद्ध के इसी औचित्य का वर्णन एक अन्य स्थान पर जालूत (गोलियथ) की उद्दंडता और हज़रत दाऊद के हाथों उसकी हत्या का उल्लेख करते हुए इस तरह किया गया है:
وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ.(البقرہ : ۲۵۱)
“अगर अल्लाह लोगों का एक दूसरे के माध्यम से विनाश न करता तो ज़मीन फ़साद से भर जाती, मगर दुनियावालों पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है।” (कि वह फ़साद के अंत की व्यवस्था करता रहता है।) (अल-बकरा: 251)
एक अन्य स्थान पर राष्ट्रों की परस्पर शत्रुता का उल्लेख करते हुए कहा गया है:
ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًۭا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًۭا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ. (المائدہ : ۶۴)
“जब भी वे जंग और ख़ून खराबे की आग भड़काते हैं, तो अल्लाह उसे बुझा देता है, और वे ज़मीन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह फ़साद करने वालों को पसन्द नहीं करता।” (अल-माइदा: 64)
अल्लाह की राह में जिहाद
यही बिगाड़ और अशांति, लालच और हवस, द्वेष और दुश्मनी, कट्टरता और संकीर्णता की लड़ाई है, जिसकी आग को ठंडा करने के लिए अल्लाह ने अपने नेक बंदों को तलवार उठाने का आदेश दिया है। कहा गया:
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ.(الحج : ۴۰-۳۹)
“जिन लोगों के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है उन्हें लड़ने की अनुमति दी जाती है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, और अल्लाह वास्तव में उनकी सहायता करने में समर्थ है। ये वे लोग हैं जिन्हें बिना किसी अपराध के उनके घरों से निकाल दिया गया है, उनका दोष बस यह था कि वे अल्लाह को अपना पालनहार कहते थे।” (अल-हज : 39-40)
यह क़ुरआन की पहली आयत है जो लड़ाई के बारे में उतरी है। इसमें जिन लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध का आदेश दिया गया है, उनका दोष यह नहीं बताया गया कि उनके पास एक उपजाऊ देश है, या उनके पास व्यापार की बड़ी मंडी है, या वे दूसरे धर्म का पालन करते हैं, बल्कि उनका अपराध स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि वे अत्यचार करते हैं, निर्दोष लोगों को उनके घरों से निकाल देते हैं, और वे इतने कट्टर हैं कि वे उन्हें केवल अल्लाह को पालनहार कहने पर प्रताड़ित करते हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ केवल आत्मरक्षा में युद्ध का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें अन्य उत्पीड़ित लोगों की सहायता और समर्थन करने का भी आदेश दिया गया है, और इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कमज़ोर और असहाय लोगों को अत्याचारियों के चंगुल से छुड़ाया जाए।
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (النساء: ۷۵)
“तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें इस बस्ती से निकाल, जहाँ के लोग बहुत ज़ालिम और अत्याचारी हैं, और हमारे लिए ख़ास अपनी ओर से एक रक्षक और सहायक नियुक्त कर दे।” (अन्निसा :75)
ऐसा युद्ध, जो अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ आत्मरक्षा के लिए और कमज़ोर, असहाय और शोषितों की सहायता के लिए लड़ा जाता है उसे अल्लाह ने विशेष अपने मार्ग में लड़ा गया युद्ध ठहराया है। जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि यह युद्ध बन्दों के लिए नहीं है, बल्कि, ख़ास अल्लाह के लिए है, और बन्दों के प्रयोजन के लिए नहीं, परन्तु अल्लाह की विशेष प्रसन्नता के लिए है। यह युद्ध तब तक जारी रखने का आदेश दिया गया है जब तक कि स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए अल्लाह के निर्दोष बन्दों पर अत्याचार और उनका शोषण बंद न हो जाए। तो उसने कहा, “उनसे तब तक लड़ो जब तक कि फ़ितना पूरी तरह मिट न जाए।” और “जब तक कि युद्ध अपने हथियार न डाल दे और अब बिगाड़ को मिटाने के लिए युद्ध की कोई ज़रूरत बाक़ी न रहे। साथ ही यह भी बताया गया है कि सत्य पर आधारित इस युद्ध को रक्तपात छोड़ देने या इसमें जान-माल की हानि देखकर युद्ध को त्याग देने का परिणाम कितना बुरा होता है।
सत्य और असत्य की सीमा
अल्लाह सर्वशक्तिमान ने सत्य के समर्थन के युद्ध की समीचीनता और आवश्यकता जताने और उसपर बल देने पर ही बस नहीं किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि:
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا(النساء: ۷۶) .
“जो लोग ईमान लाये, वे अल्लाह की राह में युद्ध करते हैं और जो काफ़िर हैं, वे उपद्रव के लिए युद्ध करते हैं। तो शैतान के साथियों से युद्ध करो। निःसंदेह शैतान की चाल निर्बल होती है।” (अन्निसा :76)
यह एक अध्यादेश है जिसमें सत्य और असत्य के बीच पूरी तरह से सीमांकन कर दिया गया है। जो लोग अन्याय और उपद्रव के लिए युद्ध करते हैं वे शैतान के साथी हैं, और जो अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए लड़ते हैं वे अल्लाह के मार्ग के योद्धा हैं। ऐसा प्रत्येक युद्ध जिसका उद्देश्य सच्चाई और न्याय के विरुद्ध अल्लाह के बन्दों को छति पहुँचाना है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित करना है, जिसका उद्देश्य उन निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करना है जो अल्लाह का नाम लेते हैं, वह शैतान के नार्ग की लड़ाई है और यह अल्लाह के विरुद्ध है। ऐसा युद्ध लड़ना अल्लाह पर ईमान रखने वालों का काम नहीं है। इसके विपरीत जो लोग अत्याचारियों के ख़िलाफ़ पीड़ितों और शोषितों का समर्थन और बचाव करते हैं, जो दुनिया से अत्याचार और विद्रोह को मिटाकर न्याय और शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो अल्लाह के बन्दों को शांति और संतोष में रहने और मानवता के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ने का अवसर देने के लिए विद्रोहियों और दंगाइयों की जड़ें काट देते हैं, उनका युद्ध अल्लाह के मार्ग का युद्ध है। वे कैसे पीड़ितों की मदद करते हैं जैसे कि ख़ुद अल्लाह की मदद कर रहे हों। उन के लिए ही अल्लाह की मदद का वादा है।
अल्लाह के मार्ग में जिहाद की उत्कृष्टता
यह वही अल्लाह के मार्ग में जिहाद है, जिसकी उत्कृष्टता क़ुरआन में जगह-जगह बयान की गई है। जिसके बारे में कहा गया है:
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الصف: ١٠-١١)
“ऐ ईमान वालों! क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा व्यापार बताऊँ जो तुम्हें दुखदायी यातना से बचा ले? वह व्यापार यह है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करो । यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, अगर तुम जानो।” (अल-सफ :10-11)
जिसमें सेनानियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
اِنَّ اللّـٰهَ يُحِبُّ الَّـذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِـه صَفًّا كَاَنَّـهُـمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ۔ (الصف : ۴)
“निःसंदेह अल्लाह प्रेम करता है उनसे, जो उसकी राह में पंक्तिबंद होकर युद्ध करते हैं, जैसे कि वे सीसा पिलाई दीवार हों।” (अल-सफ: 4)
“जिसकी महिमा और बड़ाई की गवाही ऐसे दी गई है:
اجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جَهَدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ و أوليكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبه : ۱۹ - ۲۰)
“क्या तुम ह़ाजियों को पानी पिलाने और सम्मानित मस्जिद (काबा) की सेवा को, उन लोगों के (ईमान के) बराबर समझते हो, जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के समीप दोनों बराबर नहीं हैं तथा अल्लाह अत्याचारियों का मार्गदर्शन नहीं करता। जो लोग ईमान लाये और सत्य के लिए घर-बार छोड़ा और अल्लाह की राह में अपने अपनी जान और धनों से जिहाद किया, उनका पद अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है और वही वास्तव में सफल हैं।” (अल- तौबा :19-20)
यही वह सत्य की लड़ाई है जिसमें एक रात जागना हज़ार रातों की इबादत करने से बढ़कर है, जिस के मैदान में जम कर खड़े होना 60 साल तक नमाज़ अदा करते रहने से बेहतर बताया गया है, जिसमें जागने वाली आँख पर जहन्नम की आग हराम है, जिनके मार्ग में धूल से सनने वाले क़दमों से वादा किया गया है कि वे कभी भी नरक की ओर नहीं घसीटे जाएंगे, और इस के साथ ही उन लोगों को, जो इस से बचकर घर बैठ जाएं और उसकी पुकार सुनकर क़समसाने लगें, डांट सुनाई गई है।
قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ۔(التوبہ: ۲۴)
“ऐ नबी! कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी पत्नियाँ, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यपार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है तथा वे घर जिनसे तुम मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय हैं, तो प्रतीक्षा करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाये और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता।” (अत्तौबा :24)
जिहाद की उत्कृष्टता का कारण
ग़ौर कीजिए कि अल्लाह की राह में जिहाद की इतनी उत्कृष्टता और तारीफ़ किस लिए है? जिहाद करने वालों को बार-बार क्यों कहा जाता है कि वे ही सफल हैं और उनका ही रुतबा ऊंचा है? और इस से बचकर घर बैठने वालों को ऐसी चेतावनी क्यों दी जाती है? इस प्रश्न को हल करने के लिए जरा उन आयतों पर ग़ौर करें जिनमें जिहाद का आदेश और उसकी खूबियां और उससे भागने की बुराइयां लिखी हुई हैं। उन आयतों में किसी भी स्थान पर उत्कृष्टता का अर्थ धन-दौलत और सत्ता-साम्राज्य की प्राप्ति नहीं बताया गया है।
जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था :
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय:
(गीता, अध्याय-2, श्लोक-37)
या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्ध के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा।
इस प्रकार क़ुरआन में कहीं अल्लाह की राह में लड़ने को यह कहकर प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि बदले में तुम्हें दुनिया की दौलत और सत्ता मिलेगी। इसके विपरीत अल्लाह की राह में जिहाद के बदले हर जगह केवल ख़ुदा की प्रसन्नता और ख़ुदा की नज़र में ऊँचे स्थान की उम्मीद और दुखदायी यातना से सुरक्षित रहने की उम्मीद दिलाई गई है।
अल्लाह के घर (काबा), जहां मुहम्मद (सल्ल.) के नबी बनने से पहले भी दूर दराज़ से लोग हज और उमरा करने आते रहते थे, वहां हाजियों की सेवा करना, उन्हें पानी पिलाना और काबा की व्यवस्था देखना बड़े प्रभावशाली और मोटी आमदनी के पद थे, उन सब को और अपने घर बार को छोड़ देने और अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने को श्रेष्ठ बताया गया। फिर उसके बदले में अल्लाह की दृष्टि में सर्वोच्च पद के अलावा किसी इनाम का उल्लेख नहीं किया गया।
एक और जगह एक व्यापार का गुर सिखाया गया, जिससे यह आभास होता है कि संभवत: यहां कुछ धन-सम्पत्ति का उल्लेख हो, लेकिन जब आप पढ़ें और देखें, तो इस व्यापार की वास्तविकता यह है कि अपना जीवन और धन अल्लाह की राह में ख़र्च करो, और उसके बदले में नरक की यातना से छुटकारा पाओ। एक अन्य स्थान पर लड़ाई से जी चुराने वाले को इस बात पर डाँटा जा रहा है कि वे पत्नियों और बच्चों के मोह में फँसे हुए हैं और अपनी अर्जित संपत्ति के नष्ट होने और अपने व्यापार के घाटे और अपने प्यारे घरों के छिन जाने से भयभीत हैं। हालांकि संसार में युद्ध करके देशों को जीतने वालों को धन-सम्पत्ति मिलती है, उनका व्यापार भी चमक उठता है और उन्हें जीते हुए लोगों से ली गई भव्य इमारतों भी रहने को भी मिलती हैं।
जब इस जिहाद का मक़सद दुनिया की दौलत और साम्राज्य विस्तार नहीं है तो अल्लाह को इस ख़ून खराबे से क्या मिलता है कि वह इसके बदले में इतने ऊंचे-ऊंचे पद दे रहा है? आख़िर इस ख़तरनाक काम में क्या रखा है कि इसके लिए धूल-धूसरित होने वाले को अनुग्रह और उपकार का पात्र बनाया जाता है? आख़िर इसमें ऐसी कौन सी सफलता निहित है, कि जो लोग इस नीरस और अरुचिकर युद्ध में भाग लेते हैं, उन्हें बार-बार “यही लोग कामयाब हैं” कहा जा रहा है? इसका उत्तर “और यदि अल्लाह कुछ लोगों के ज़रिये कुछ लोगों को हटाता न रहता, तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती।” (क़ुरआन) और “और यदि तुम ऐसा न करोगे, तो धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ उत्पन्न हो जायेगा।” (क़ुरआन) में छिपा है। अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन पर उत्पात और बिगाड़ फैले। वह नहीं चाहता कि उसके निर्दोष बन्दों को सताया जाए और कष्ट दिया जाए। वह बलवान द्वारा निर्बल को फाड़ खाना, उनकी शांति को और उनके नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को नष्ट करना पसन्द नहीं करता। वह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि संसार में क्रूरता और अन्याय हो और हत्याएं होती रहें। उसे यह पसंद नहीं है कि उसके बन्दों को उसके बन्दों का दास बनाया जाए और उनकी मानव गरिमा को कलंकित किया जाए। इसलिए जो समुदाय बिना किसी इनाम की इच्छा के, बिना किसी धन के लालच के, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के, केवल अल्लाह के लिए, दुनिया को इस बिगाड़ से मुक्त करने और इस अत्याचार को दूर करने और इसके स्थान पर न्याय स्थापित करने के लिए खड़ा हो जाए। इस अच्छे काम के लिए अपने जीवन और संपत्ति, अपने व्यापार के मुनाफ़े, अपने बाल, बच्चों और अपने माता-पिता और भाइयों के प्यार, और अपने घर की विलासिता, सब कुछ, बलिदान कर दे, उससे बढ़कर और कौन अल्लाह की स्वीकृति का पात्र हो सकता है?
अल्लाह की राह में जिहाद की यही फ़ज़ीलत है, जिसके आधार पर इसे अल्लाह पर ईमान लाने के बाद सभी इंसानी कामों में सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह सभी गुणों और नैतिक मूल्यों की आत्मा है। मनुष्य की यह भावना कि वह किसी भी परिस्थिति में बुराई को बर्दाश्त न करे और उसे दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए तैयार हो जाए मानव श्रेषठता की उच्चतम भावना है। और व्यावहारिक जीवन में सफलता का रहस्य भी इसी भावना में निहित है। दूसरों की बुराई को सहन करने वाले व्यक्ति की नैतिक कमज़ोरी अंततः उसे अपने लिए बुराई सहन करने की ओर ले जाती है। और जब उसमें सहनशीलता का यह तत्व निर्मित हो जाता है, तब उस पर उस स्तर की दीनता आ जाती है, जिसे अल्लाह ने अपने कोप के रूप में परिभाषित किया है :
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّـهِ ۗ
और उनपर अपमान तथा तिरस्कार थोप दी गयी और वे अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। (अल-बक़रह : 61)
इस स्तर तक पहुँचने के बाद, एक व्यक्ति में शालीनता और मानवता की भावना नहीं रह जाती है। वह केवल शारीरिक और भौतिक ग़ुलामी ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ग़ुलामी में भी लिप्त हो जाता है और नीचता के ऐसे गड्ढे में गिर जाता है जिससे बाहर निकलना असंभव हो जाता है। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति में यह नैतिक शक्ति हो कि वह बुराई को केवल इसलिए बुरा मान ले कि वह बुराई है और मानव समुदाय को उससे छुटकारा दिलाने के लिए अथक प्रयास करता रहे, वही सच्चा और उच्च श्रेणी का मनुष्य होता है और उसका अस्तित्व समस्त मानवजाति के लिए एक वरदान होता है। ऐसा इंसान भले ही दुनिया से कोई मुआवज़ा न चाहे, लेकिन दुनिया अपनी सारी अकृतज्ञता के बावजूद भलाई से इतनी अंजान नहीं है कि इंसानियत के उस सेवक को अपना सरदार और अपना नेता स्वीकार न करे। इसी से उस आयत का अर्थ समझ में आता है, जिसमें कहा गया है कि ज़मीन के उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी बन्दे होंगे। यहीं से यह बात भी निकलती है कि... ये ही लोग सफल हैं। इससे आशय केवल परलोक की सफलता ही नहीं है, बल्कि इस संसार की सफलता भी वास्तव में उन्हीं लोगों के लिए है, जो निज स्वार्थ से ऊपर उठकर, केवल अल्लाह की प्रसन्नता और अल्लाह के बन्दों की भलाई के लिए जिहाद करते हैं।
सभ्यता के प्रयोजन में जिहाद का महत्व
जिहाद की इस सच्चाई को जान लेने के बाद यह समझना बहुत आसान है कि राष्ट्रों के जीवन में इसका क्या महत्व है और सभ्यता की व्यवस्था को सही रखने के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर दुनिया में कोई ऐसी ताक़त है जो बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद छेड़ती रहे और सभी उपद्रवी ताक़तों को अपनी मर्यादा में रहने के लिए मजबूर करती रहे, तो सभ्य व्यवस्था में यह असंतुलन बिल्कुल दिखाई न दे। आज पूरी दुनिया अत्याचारियों और पीड़ितों, आक़ओं और ग़ुलामों में बंटा हुआ है और पूरी दुनिया का नैतिक और आध्यात्मिक जीवन ग़ुलामी और दमन और उत्पीड़न के कारण नष्ट हो रहा है। बुराई को दूसरों से दूर करना तो बड़ी बात है, अगर किसी राष्ट्र में स्वयं से बुराई को दूर करने की भावना भी मौजूद हो और उसके लिए वह अपनी विलासिता और अपनी सुख-समृद्धि को त्याग करने के तैयार हो तो वह कभी अपमानित नहीं हो सकता। कोई ताक़त उसकी ईज़्ज़त और उसके सम्मान को नष्ट नहीं कर सकती। सत्य के आगे सिर झुकाना और असत्य के आगे सिर झुकाने की जगह मौत को तरजीह देना एक प्रतिष्ठित कौम की पहचान होनी चाहिए। अगर उसमें सत्य को स्थापित करने और सत्य की सहायता करने की ताक़त नहीं हो तो उसे कम से कम सत्य की सुरक्षा के काम पर मज़बूती से जमे रहना चाहिए, जो प्रतिष्ठा का निम्नतम स्तर है। इस स्तर से गिर कर जो राष्ट्र सत्य की सुरक्षा भी न कर सके और उसमें बलिदान का अभाव इस हद तक बढ़ जाए कि जब बुराई और दुष्टता उस पर चढ़ आए तो वह उसे नष्ट करने या स्वयं नष्ट होने के स्थान पर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर ले तो ऐसे राष्ट्र के लिए दुनिया में कोई सम्मान नहीं है। उसका जीवन निश्चित रूप से मृत्यु से भी बदतर है। इसी रहस्य को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने किताब में बार-बार उन राष्ट्रों का उल्लेख किया है जिन्होंने बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करने में जान व माल का घाटा देख कर उस से जी चुराया और बुराई का आधिपत्य स्वीकार कर के अपने ऊपर हमेशा के लिए कायरता और नपुंसकता का दाग़ लगा लिया। अल्लाह ऐसे राष्ट्रों को अत्याचारी राष्ट्र कहता है। अर्थात्, उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं पर अत्याचार किया, और वास्तव में वे अपने ही अत्याचारों से नष्ट हो गए। उनका उदाहरण एक जगह इस प्रकार दिया गया है:
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَـٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَـٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۔ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ۔ (التوبہ : ۷۰-۷۱)
“क्या इन्हें उन क़ौमों के समाचार नहीं पहुँचे, जो इनसे पहले थे; नूह़, आद, समूद तथा इब्राहीम की क़ौम और मद्यन के निवासियों और उन बस्तियों के, जो पलट दी गईं? उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ ले कर आये। अल्लाह ने उनपर अत्याचार नहीं किया, परन्तु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ईमान वाले पुरुष और स्त्रियाँ एक-दूसरे के सहायक हैं। वे भलाई का आदेश देते तथा बुराई से रोकते हैं।” (अत्तौबा :70-71)
यहाँ, पिछली क़ौमों के अपने ऊपर अत्याचार का उल्लेख करते ही, जो ईमान वालों का यह गुण बताया है कि वे एक दूसरे के सहायक और सहयोगी होते हैं, अच्छाई की स्थापना करते हैं और बुराई को रोकते हैं, तो इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उन मिटने वाले राष्ट्रों ने अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना बंद कर दिया था, और यही वह अत्याचार था जिसने अंततः उन्हें नष्ट कर दिया।
एक अन्य स्थान पर बनी इसराईल की कायरता और जिहाद से भागने का वर्णन किया गया है। कहा कि अल्लाह के मबी हज़रत मूसा ने अपनी क़ौम को अल्लाह की कृपाएं याद दिलाकर उन्हें आदेश दिया कि तुम पवित्र भूमि में प्रवेश कर जाओ, जिसे अल्लाह ने तुमको विरासत में दे दिया है, और कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, क्योंकि जो लोग अपनी पीठ फेरते हैं, वे हमेशा विफल रहते हैं। लेकिन बनी इसराईल (इसराईल की संतान, अर्थात् यहूदी) के मन में आतंक बैठा हुआ था, उन्होंने कहा:
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًۭا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ۔ (المائدہ : ۲۲)
“उन्होंने कहाः हे मूसा! उसमें बड़े बलवान लोग रहते हैं और हम उसमें कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक वे उस से निकल न जायें, यदि वे निकल जाते हैं, तभी हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं।” (अल-माइदा :22)
क़ौम के दो बहादुरों ने, जिन पर अल्लाह का इनाम था, क़ौम को नसीहत की कि तुम निडर होकर प्रवेश कर जाओ, तुम ही जीतोगे, अगर तुम्हारे पास ईमान की दौलत है तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन वह कायर और अपमान पर संतुष्ट रहने वाली क़ौम मनुष्यों के भय से कांपती ही रही और उसने स्पष्ट कह दिया कि:
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًۭا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَـٰتِلَآ إِنَّا هَـٰهُنَا قَـٰعِدُونَ۔ (المائدہ : ۲۴)
“वे बोलेः हे मूसा! हम उसमें कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक वे उसमें (उपस्थित) रहेंगे, अतः तुम और तुम्हारा पालनहार जाओ, फिर तुम दोनों युद्ध करो, हम यहीं बैठे रहेंगे।” (अल-माइदा :24)
फिर इस कायरता के कारण अल्लाह ने यह निर्णय किया कि वे चालीस वर्षों तक दर-बदर की धूल छानते फिरें और उन्हें कहीं भी ठिकाना न मिल पाए:
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةًۭ ۛ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ (المائدہ :۲۶)
अल्लाह ने कहाः वह (भूभाग) जो उनके लिए लिख दिया गया था. चालीस वर्षों के लिए उनपर ह़राम (वर्जित) कर दिया गया। अब वे धरती में भटकते फिरेंगे। (अल-माइदा: 26)
एक दूसरी जगह विस्तार के साथ बनी इसराईल की उस कायरता और मौत के डर का उल्लेख किया गया है, जिसके कारण उन्होंने अल्लाह के मार्ग में जिहाद को छोड़ दिया था और जिस के कारण अंततः उन्हें राष्ट्रीय विनाश का सामना करना पड़ा। कहा गया है:
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۔ (البقره: ۲۴۳)
“क्या तुमने उन लोगों की दशा पर विचार नहीं किया, जो अपने घरों से मौत के भय से निकल गये, जबकि उनकी संख्या हज़ारों में थी, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। वास्तव में, अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उपकारी है, परन्तु अधिकांश लोग कृतज्ञता नहीं करते।” (अल-बक़रह : 243)
उसके बाद, मुसलमानों को इस प्रकार लड़ने का आदेश दिया गया:
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ۔ (البقره: ۲۴۴)
“अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो और जान लो कि वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।”(अल-बकराः 244)
और उसके बाद बानी इसराईल के एक समूह का फिर ज़िक्र आता है:
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰٓ إِذْ قَالُوا۟ لِنَبِىٍّۢ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًۭا نُّقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَـٰتِلُوا۟ ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَـٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ۔ (البقره: ۲۴۶)
“क्या तुमने बनी इसराईल के एक समूह के विषय पर विचार नहीं किया, जो मूसा के बाद सामने आया? जब उसने अपने नबी से कहाः हमारे लिए एक राजा बना दो। हम अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे, (नबी ने) कहाः कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया जाये तो तुम अवज्ञा करने लगो? उन्होंने कहाः ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह की राह में युद्ध न करें। जबकि हम अपने घरों से निकाल दिये गये हैं और अपनी संतान से अलग कर दिये गये हैं।परन्तु, जब उन्हें युद्ध का आदेश दे दिया गया, तो उनमें से थोड़े के सिवा सब फिर गये। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भाँति जानता है।” (अल-बकरा: 246)
ये और कई अन्य उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए बार-बार दिए गए हैं कि सद्गुण की स्थापना और उसे बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ उसकी रक्षा के लिए सच्चे बलिदान की भावना है। और जिस राष्ट्र से यह भावना निकल जाती है वह बहुत जल्दी बुराई से पराजित होकर मिट जाता है।
दूसरा अध्याय
रक्षात्मक युद्ध
पिछली चर्चा से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि क़ुरआन की शिक्षा अपने मानने वालों में सत्य के समर्थन की ऐसी अजेय भावना पैदा करना चाहती है कि उनमें किसी भी स्थिति में बुराई और अत्याचार के सामने सर झुकाने और अन्याय एवं उद्दंडता के प्रभुत्व को स्वीकार करने की कमज़ोरी पनपने न पाए। क़ुरआन की शिक्षाओं के अनुसार इंसान का सबसे बड़ा अपमान यह है कि वह अपने भोग विलास, धन सम्पत्ति और बाल बच्चों के मोह में पड़कर सत्य की रक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से डरने लगे और असत्य को शक्तिशाली देखकर उसकी ग़ुलामी स्वीकार करने को तैयार हो जाए। यह दुर्बलता वास्तव में शरीर की दुर्बलता नहीं बल्कि हृदय और विश्वास की दुर्बलता है। जब यह किसी राष्ट्र में पैदा हो जाती है तो उसके भीतर से सम्मान और प्रतिष्ठा के सारे भाव स्वत: निकल जाते हैं। फिर सत्य की सेवा करना ते दूर, वह ख़ुद को सत्य के रास्ते पर भी नहीं रख पाता। लोग समझते हैं कि शरीर की ग़ुलामी का प्रभाव केवल ऊपर ऊपर रहता है और दिल और आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तथ्य यह है कि शरीर के ग़ुलाम बनने से पहले, आत्मा ग़ुलाम हो चुकी होती है। शरीर ग़ुलामी के अपमानजनक परिधान को धारण ही तब करता है जब आत्मा सम्मान और गरिमा से वंचित हो चुकी होती है।
जो राष्ट्र अपनी दुर्बलता और कायरता के कारण अपने अधिकारों की रक्षा में लापरवाही करता है और बुराई को शक्तिशाली देखकर, उसका पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें यह शक्ति कभी नहीं रहती है कि वह अपने संस्कारों, अपने सिद्धांत और क़ानूनों और अपनी धार्मिक नैतिकता पर मज़बूती से जमा रहे, और अपनी सामुदायिक व्यवस्था को टूटने न दें। फिर जब सत्य और असत्य एक दूसरे के विपरीत हैं और एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते तो एक राष्ट्र असत्य की दासता को स्वीकार करके और आज्ञापालन का सम्बन्ध बनाकर भी सत्य की बन्दगी में कैसे रह सकता है? सत्य का स्वभाव एक्यप्रिय होता है, वह असत्य को कभी भी अपने साझी बनाकर कभी ऐसा विभाजन नहीं कर सकता कि आधा मेरा है और आधा तेरा। इसलिए, जो कोई भी इसकी बन्दगी करना चाहता है, उसे असत्य की बन्दगी छोड़नी होगी और अपनी गर्दन को अन्य सभी बन्दगियों के पट्टे से मुक्त रखना पड़ेगा।
कुरआन, जो वास्तव में कुदरत का धर्मग्रंथ है, कुदरत के इस रहस्य को पूरी तरह से निहित रखता है। इस कारण उसने मनुष्य को दो ही मार्ग बताए हैं, या मृत्यु, या प्रतिष्ठा, उसने प्रतिष्ठाविहीन जीवन का तीसरा मार्ग नहीं बताया। यह अलग बात है कि उसके बदनसीब अनुयायियों ने अपने ईमान की दुर्बलता और साहस की कमी के कारण उसे अपना लिया हो। वह तो उस जीवन को “अपमान और असफलता” के रूप में वर्णित करता है, उसे अल्लाह का प्रकोप बताता है, और इसे उन राष्ट्रों की विशेषता के रूप में वर्णित करता है, जो अपनी कायरता और अल्लाह के सिवा दूसरों से डरने के कारण ख़ुद को अल्लाह के प्रकोप का पात्र बना लेते हैं। कुरआन ने ऐसे लोगों को घाटे और विफलता की धमकी सुनाई है:
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا۔ (النساء :۹۷)
“निःसंदेह वे लोग, जिनके प्राण फ़रिश्ते निकालते हैं, इस दशा में कि वे अपने ऊपर (कुफ़्र के देश में रहकर) अत्याचार करने वाले हों, तो उनसे कहते हैं, तुम यह किस हाल में जी रहे थे? वे कहते हैं कि हम धरती में विवश थे। तब फ़रिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि तुम उस जगह को छोड़ कर कहीं और निकल जाते? तो इन्हीं का ठिकाना नरक है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है।”(अन्निसा : 97)
ए यह आयत उन मुसलमानों के बारे में नाज़िल हुई जो पैग़म्बर (सल्ल.) और आम मुसलमानों की हिजरत (मदीना प्रवास) के बाद मक्का में रह गए थे और जिन्होंने अपने घरों, अपने व्यवसायों और अपनी संपत्तियों के लिए असत्य के उस माहौल में रहना स्वीकार कर लिया था, जिसमें वे अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार इस्लामी जीवन नहीं जी सकते थे, बल्कि अवज्ञाकारियों द्वारा उत्पीड़ित होने के कारण उसे कई अवज्ञाकारी तरीक़े अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, यहाँ तक कि इसी दबाव के कारण उन्हें अंततः अवज्ञाकारियों की सेना में शामिल होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बद्र के मैदान में आना पड़ा।
ग़ौर कीजिए कि सामुदायिक प्रतिष्ठा की यह कैसी उज्जवल शिक्षा है। अपने को कमज़ोर समझकर असत्य के अनुपालन पर राजी हो जाने वालों को अत्याचारी कहा जा रहा है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने यह अपमान क्यों स्वीकार किया? वे कमज़ोरी और दुर्बलता का बहाना बनाते हैं तो वह स्वीकार नहीं किया जाता। उत्तर यह मिलता है कि अगर तुम कमज़ोर ही थे तो इस अपमान को स्वीकार करने के बजाय बेहतर यही होता कि अपना घर छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर चले जाते जहां तुमको अपनी आस्था और विवेक के विरुद्ध जीने के लिए मजबूर न किया जाता। तुमने अपने आराम के लिए असत्य की दासता का अपमान क्यों स्वीकार किया? अंत में इस अपराध के कारण उन्हें अपमान और विफलता के उस गर्त में फेंक दिया जाता है जिसे नरक कहा जाता है, और निश्चित रूप से उससे बुरा ठिकाना और कोई नहीं है।
रक्षात्मक युद्ध की धार्मिक बाध्यता
यही कारण है कि पवित्र क़ुरआन ने सभी मामलों में धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा दी है, लेकिन ऐसे किसी भी हमले को सहन करने की शिक्षा नहीं दी है, जो इस्लामी जीवन व्यवस्था को मिटाने और मुसलमानों पर इस्लाम के सिवा किसी अन्य व्यवस्था को थोपने के लिए किया जाए। उसने सख़्त आदेश दिया है कि जो कोई भी तुम्हारे मानवाधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तुम पर अत्याचार करे, तुमको तुम्हारी जायदादों से बाहर निकाले, तुमको तुम्हारे धर्म के अनुसार जीवन गुज़ारने से रोके, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करना चाहे, तो उसके मुक़ाबले में कोई कमज़ोरी न दिखाओ और अपनी पूरी ताक़त उस के अत्याचार को मिटाने में लगा दो।
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩١ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٩٢ وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَـٰتُ قِصَاصٌۭ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۔ (البقره: ۱۹۰-۱۹۴)
“तथा अल्लाह की राह में, उनसे युद्ध करो, जो तुमसे युद्ध करते हों और अत्याचार न करो, अल्लाह अत्याचारियों को पसंद नहीं करता। उन ज़ालिमों की हत्या करो, जहाँ पाओ और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फ़ितना (उपद्रव), हत्या करने से भी बुरा है और उनसे प्रतिष्ठित मस्जिद के पास युद्ध न करो, जब तक वे तुमसे वहाँ युद्ध न करें। परन्तु, यदि वे तुमसे युद्ध करें, तो उनकी हत्या करो, यही काफ़िरों का बदला है। फिर यदि वे (आक्रमण करने से) रुक जायें, तो अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान् है। तुम उनसे बरीबर युद्ध करते रहो, यहाँ तक कि फ़ितना न रह जाये और धर्म केवल अल्लाह के लिए रह जाये, फिर यदि वे रुक जायें, तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठित महीने, प्रतिष्ठित महीने के बदले है और सभी प्रतिष्ठा और सम्मान का बदला है। (यानी जिस महीने और जिस जगह की पवित्रताएं स्थापित की गई हैं, उन का पालन उसी स्थिति में किया जाएगा जब दुश्मन भी उन का पालन करेगा।) अतः, जो तुमपर अतिक्रमण (अत्याचार) करे, तो तुम भी उसपर उसी के समान (अतिक्रमण) करो तथा अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह केवल उन्हीं के साथ है, जो उसकी अवज्ञा के परिनाम से डरते हैं।” (अल-बक़रह : 190-194)
दीन की रक्षा और इस्लाम की भूमि की रक्षा का यह आदेश इतना सख़्त है कि जब कोई भी ताक़त इस्लाम को नष्ट करने और इस्लामी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए हमला करती है, तो सभी मुसलमानों पर यह अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने सभी काम छोड़ दें और इसके मुक़ाबले के लिए निकल आएं, और जब तक इस्लाम और इस्लामी व्यवस्था को इस खतरे से सुरक्षित न कर लें, तब तक चैन न लें। इसलिए, फ़िक़्ह (इस्लामी धर्मशास्त्र) की सभी किताबों में, यह आदेश मौजूद है कि जब दुश्मन दारुल-इस्लाम (इस्लामी राज्य) पर हमला करता है, तो मुसलमानों पर नमाज़ और रोज़ा जैसी इबादतों की तरह रक्षा का दायित्व भी अनिवार्य हो जाता है। इस्लामी फ़िक़्ह की जानी मानी किताब ‘बदायअ अस्सनायअ’ में लिखा है :
“मगर, जब यह सार्वजनिक घोषणा हो जाए कि दुश्मन ने किसी इस्लामी राज्य पर हमला किया है, तो फिर जिहाद अनिवार्य हो जाता है और जिहाद की शक्ति रखने वाला हर मुसलमान व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य होता है। सार्वजनिक घोषणा हो जाने के बाद जिहाद करने के लिए हर किसी के खड़े हुए बिना फर्ज पूरा नहीं होता। उस समय, यह सभी मुसलमानों पर इस तरह अनिवार्य हो जाता है, जैसे रोज़ा और नमाज़। अत: दास को अपने स्वामी की अनुमति के बिना और एक महिला को अपने पति की अनुमति के बिना निकलना चाहिए, क्योंकि उन इबादतों में, जो फ़र्ज़े ऐन (अति अनिवार्य) हैं दास और पत्नी पर स्वामी और पति के अधिकार से ऊपर हैं। इसी तरह बेटे को माता-पिता की अनुमति के बिना बाहर जाने की अनुमति है, क्योंकि रोज़ा और नमाज़ जैसे अनिवार्य दायित्वों में माता-पिता का अधिकार प्रभावी नहीं होता है।” (खंड 7. पृष्ठ 98)
इसमें जो शब्द आए हैं वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह दायित्व केवल इस मामले तक ही सीमित नहीं है कि एक विशेष धार्मिक भावना से प्रभावित एक राष्ट्र इस्लाम को नष्ट करने के लिए हमला करे, बल्कि इस्लामी राज्य के अतिक्रमण के लिए किए जाने वाले हमले के मामले में भी यह इसी तरह अनिवार्य है। इस्लाम में मुसलमानों के राष्ट्रीय जीवन के लिए स्वतंत्रता और स्थायित्व सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अपनी आज़ादी खोने के बाद, केवल यही नहीं कि मुसलमानों में मानवता के सर्वोच्च दायित्व को पूरा करने की योग्यता नहीं रह जाती है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें पैदा किया गया है, बल्कि वे अपनी शरिया व्यवस्था को भी बनाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं, जिनपर उनका धार्मिक जीवन निर्भर है। इसलिए इस्लामी हुकूमत और इस्लामी राष्ट्रीयता पर हमला करना इस्लाम की बुनियाद पर हमला है। भले ही दुश्मन का मक़सद इस्लाम का सफ़ाया करना न हो, बल्कि मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति को मिटाना हो, तब भी, उसके ख़िलाफ़ लड़ना मुसलमानों के लिए वैसे ही अनिवार्य है जैसा इस्लाम के विध्वंसक के ख़िलाफ़ लड़ना अनिवार्य है। इसी वजह से केवल उसी शहर या राज्य के मुसलमानों पर ही रक्षा का दायित्व नहीं डाला गया है जिस शहर या जिस राज्य पर हमला किया गया हो, बल्कि अगर वे अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हों तो दुनिया के सभी मुसलमानों पर अनिवार्य कर दिया गया है कि वे उस देश या शहर के मुसलमानों को दुश्मन के प्रभुत्व से बचाएं। निहाया के लेखक ने संग्रह से इस सारांश का विवरण इस प्रकार किया है:
सच तो यह है कि जब नफ़ीर (सार्वजनिक घोषणा) हो जाए तो जिहाद केवल उन लोगों पर अनिवार्य होता है जो दुश्मन के क़रीब हों। रही बात उन लोगों की जो दुश्मन से दूर हैं तो उन पर यह फ़र्ज़े कफ़ाया (सशर्त अनिवार्य) होता है। यानी अगर उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो वे जिहाद में भाग लेने से बच सकते हैं। लेकिन अगर उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे इसलिए कि जो लोग दुश्मन के क़रीब थे वे लड़ने में असमर्थ हो गए या इसलिए कि वे कमज़ोर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताक़त से मुक़ाबला नहीं किया। इस स्थिति में, आस-पास के लोगों पर जिहाद वैसा ही पूर्ण दायित्व बन जाता है, जैसे नमाज़ और रोज़े, कि इसे छोड़ना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, फिर उन लोगों पर जो उनके क़रीब हों, फिर उन लोगों पर जो उनके क़रीब हों, यहाँ तक कि पूर्व से पश्चिम तक, इस्लाम के सभी मानने वालों पर समान क्रमिकता के साथ अनिवार्य होता चला जाता है।” (शामी, खंड 3, पृष्ठ 240)
इस्लाम में रक्षा के इस महत्वपूर्ण दायित्व की स्थिति का अंदाजा केवल इस बात से नहीं लगाया जाता, कि इसे एक इबादत और अनिवार्य दायित्व का दर्जा दिया गया है और इसका लाभ नमाज़ और रोज़े से बढ़कर बताया गया है। सूरह अत-तौबा की उन आयतों से जो तबूक की लड़ाई के बारे में नाज़िल हुई हैं, यह मालूम होता है कि जब कोई ताक़त इस्लाम और मुसलमानों की आज़ादी को तबाह करने के लिए हमला करती है और नफ़ीर आम हो जाता है, तो उस समय यह ईमाम के सच्चे या झूठे होने की कसौटी बन जाता है। इसलिए, उन लोगों के बारे में जिन्होंने रोमनों के शक्तिशाली साम्राज्य के ख़िलाफ़ इस्लाम की रक्षा के लिए युद्ध में जाने से जी चुराया था और जिनके ईमान की कमज़ोरी को देख कर, पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उन्हें घर पर बैठे रहने की अनुमति दे दी थी, ये शब्द कहे गए हैं:
عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٤٣ لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ٤٤ إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۔ (التوبه : ۴۳ - ۴۵ )
“ऐ मुहम्मद! अल्लाह तुमको माफ़ करे, तुमने उन्हें घर बैठ रहने की अनुमति क्यों दी? (तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी) ताकि जो लोग सच्चे हैं वे सामने आ जाते और उनकी स्थिति का भी पता चल जाता, जो झूठे हैं। वे लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो क़ियामत के आने वाले दिन पर ईमान रखते हैं, वे तुम से अपने माल और जान से जिहाद न करने की अनुमति कभी नहीं माँगेंगे। अल्लाह उन लोगों से भली-भांति परिचित है जो परहेज़गार हैं। इजाज़त तो वे लोग ही माँगेगे जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न उन्हें क़ियामत के दिन के आने का यक़ीन है। उनके दिलों में शक घुस चुका है, और वे शक की हालत में गुमराह हुए जा रहे हैं।” (अत्तौबा : 43-45)
रक्षात्मक युद्ध के विभिन्न रूप
रक्षा के इन नियमों से यह स्पष्ट होता है कि मुसलमानों के लिए उनकी दुनिया से संबंधित धार्मिक दायित्वों में से, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वे अपने दीन (जीवन व्यवस्था) और अपने राष्ट्रीय स्थायित्व की सख़्ती के साथ रक्षो करें। अपने राष्ट्रीय और दीनी अस्तित्व को किसी भी हाल में षडयंत्र और बिगाड़ का शिकार न होने दें। इसके लिए इस्लाम ने अपने अनुयाइयों को युद्ध की केवल अनुमति ही नहीं दी है, बल्कि उस पर ज़ोर भी दिया है और ज़ोर इतना सख़्त, कि उसकी स्थिति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है।
लेकिन हमले का मात्र यही एक रूप नहीं है कि एक साम्राज्य युद्ध की औपचारिक घोषणा करके दारुल-इस्लाम (इस्लामी राज्य) पर आक्रमण करे और उस पर विजय प्राप्त कर के मुसलमानों को ख़त्म करने, उन्हें ग़ुलाम बनाने या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी परिस्थितियाँ जो किसी राष्ट्र और उसके सामूहिक जीवन की शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकती हैं। अतः अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि वे परिस्थितियाँ क्या हैं और क़ुरआन हमें उनके बारे में क्या आदेश देता है। इस उद्देश्य के लिए, हम उन सभी आयतों को एकत्र करेंगे जिनमें रक्षात्मक युद्ध का आदेश दिया गया है, और उनके अनसुलझे मुद्दों को भी क़ुरआन से या बाद में हदीस से हल करेंगे, ताकि व्यक्तिगत विचारों के हस्तक्षेप से संदेह की जगह न हो। .
(1) क्रूरता और आक्रामकता का जवाब
क़ुरआन के एक बड़े टीकाकार के अनुसार इस्लाम में युद्ध के बारे में जो पहली आयत नाज़िल हुई, वह सूरह हज की यह आयत है:
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۔ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۔(الحج : ۳۹-۴۰)
“जिन लोगों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी जा रही है, उन्हें लड़ने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि वे शोषित हैं और अल्लाह उनकी मदद करने में सक्षम है। ये वे लोग हैं, जिन्हें उनके घरों से केवल उस दोष के लिए निकाला गया है, जो वे कहते थे: केवल अल्लाह ही हमारा पालनहार है।” (अल-हज: 39 40)
दूसरी आयत, जिसे अल्लामा इब्न जरीर और कुछ अन्य टिप्पणीकार युद्ध की पहली आयत ठहराते हैं, सूरह बक़रह की यह आयत है:
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ . وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ۔ (البقره: ۱۹۰-۱۹۱)
“अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं, और हद से आगे न बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता, और जहाँ कहीं पाओ उन्हें क़त्ल करो, और जहाँ से उन्होंने तुमको खदेड़ा है, उन्हें वहाँ से निकाल दो, इसलिए कि फ़ितना (उपद्रव), हत्या करने से भी बुरा है।” (अल-बक़रह : 190-191)
इन दो आयतों से निम्नलिखित आदेश निकलते हैं:
1. जब मुसलमानों से लड़ाई की जाए और उन पर अत्याचार किया जाए, तो उनके लिए आत्मरक्षा में युद्ध करना जायज़ है।
2. जो लोग मुसलमानों के घरों से लूट लें, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करें और उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदख़ल कर दें, तो मुसलमानों को उनसे युद्ध करना चाहिए।
3. जब मुसलमानों को उनकी धार्मिक आस्थाओं के कारण प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें केवल इसलिए सताया जाए कि वे मुसलमान हैं, तो उनके लिए जायज़ है कि वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध करें।
4. दुश्मनों ने जहां से मुसलमानों को खदेड़ दिया है, या उससे सत्ता छीन ली है, तो उस इलाक़े को फिर से हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब मुसलमानों को सत्ता मिल जाए तो उन्हें चाहिए कि दुश्मनों को उन सभी जगहों से खदेड़ दें, जहां उन्होंने मुसलमानों को निकाल दिया था।
(2) सत्य मार्ग का संरक्षण
सूरह अनफ़ाल में जिन काफ़िरों से लड़ने और उनकी जड़ें काट देने का आदेश दिया गया है, उनका एक अपराध इस प्रकार है:
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةًۭ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ۔ (الانفال :۳۶)
“जो लोग काफ़िर हैं, वे लोगों को अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए अपना माल ख़र्च करते हैं, और वे अपना माल इसी मक़सद के लिए ख़र्च करते रहेंगे, यहाँ तक कि उन्हें पछताना पड़ेगा और वे पराजित किए जाएंगे।” (अल-अनफ़ाल:36)
आगे चलकर क़ुरैश की उस सेना का, जो मुसलमानों से बद्र में लड़ने निकली थी और जिसके विरुद्ध अल्लाह ने सत्य को सत्य और असत्य को असत्य करके दिखाने के लिए अपनी विशेष सेना भेजी थी, उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:
وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًۭا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ (الانفال :۴۷)
“और उन लोगों की तरह न हो जाना जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने घरों से सीना तान कर जंग करने निकले और अल्लाह की राह से रोकते रहे।” (अल-अनफ़ाल: 47)
सूरह तौबा में फिर, उन बहुदेववादियों का अपराध जिन से युद्ध का आदेश दिया गया था, यह बताया गया है:
ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ۔ (التوبہ :۹)
“इन लोगों ने बहुत कम क़ीमत पर ईश्वरीय आयतों का सौदा किया और वे उसके रास्ते से रोकने लगे, यह बहुत बुरा काम है जो वे करते हैं।” (तौबा:9)
आगे चल कर किताबवालों (वे समुदाय जिनपर क़ुरआन से पहले की दो किताबें तौरात और बाइबिल उतारी गईं, अर्थात यहूदी और ईसाई) से लड़ने का आदेश दिया गया है कि जो लोग अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते उनसे युद्ध करो और फिर उनके अपराधों का ब्यौरा इस तरह दिया गया है:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ(التوبہ :۳۴)
“ऐ ईमान वालों! (किताबवालों में से) कई धर्माचारी (संत) और भिक्षु लोगों के धन को अवैध रूप से खाते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं।” (अत-तौबाः 34)
सूरह मुहम्मद में अधिक स्पष्टता के साथ कहा:
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍۢ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْبَـٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّبَعُوا۟ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَـٰلَهُمْ ٣ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ (محمد : ۱-۴)
“जिन लोगों ने सत्य धर्म को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और अल्लाह के मार्ग से रोकने लगे, उनके कर्मों को अल्लाह ने नष्ट कर दिया। इसलिए जब तुम्हारी उन इंकारियों से मुठभेड़ हो, तो उन की गरदनें मारो यहां तक कि उनकी ताक़त को कुचल डालो। फिर बंदियों की पकड़ मज़बूत करो और उन्हें गिरफ़्तार कर लो, फिर तुम्हें अधिकार है कि उनपर उपकार करो या फिरौती ले लो। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखो जब तक कि युद्ध अपने हथियार न डाल दे। (अर्थात युद्द की कोई ज़रूरत नहीं रह जाए।) (मुहम्मद:1-4)
इन सभी आयतों से पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते से रोकना भी एक ऐसा जुर्म है, जिसके ख़िलाफ़ जंग ज़रूरी है। अल्लाह का मार्ग से आशय अल्लाह की दी हुई जीवन व्यवस्था है, जिसे पवित्र क़ुरआन में सीधा मार्ग भी कहा गया है। और क़ुरआन की व्याख्या शैली का यह गुण है कि उसने दीन (धर्म) को एक मार्ग के रूप में परिभाषित किया। यह ऐसा है मानो यह एक ऐसा रास्ता है जो सीधे मंज़िल की ओर ले जाता है और जिस पर शैतान और शैतान के चेले धात में बैठे हैं।
अब विचार करें कि इस्लाम से रोकने का अर्थ क्या है? जब इस्लाम को एक रास्ता कहा गया तो निश्चित रूप से उसके रोकने का भी वही तरीक़ा होगा जो किसी रास्ते से रोकने का होता है। किसी रास्ते से रोकने के तीन तरीक़े हो सकते हैं। एक यह कि दूसरे रास्ते पर जाने वालों को इस रास्ते पर नहीं आने दिया जाए। दूसरा यह कि जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें जबरन यहां से हटा दिया जाए। तीसरा, उस पर चलनेवालों के मार्ग में काँटे बिछा दिए जाएं, उन्हें डराया-धमकाया और मारा-पीटा जाए ताकि वे उसपर न चल सकें। “अल्लाह के रास्ते से रोकना” के ये तीनों अर्थ हैं, लोगों को इस्लाम स्वीकार करने से रोकना, मुसलमानों को धर्मत्याग करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करना और मुसलमानों के लिए इस्लाम के अनुसार जीने को मुश्किल बना देना। क़ुरआन में इन तीन अर्थों के उदाहरण मौजूद हैं। जो समूह इस्लाम के मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करता है, उसे रास्ते से हटा देना और उसकी ताक़त को कुचल देना यह मुसलमानों का नैतिक अधिकार भी है और धार्मिक दायित्व भी।
(3) छल और वचन-भंग का दंड
एक और जुर्म जिसके ख़िलाफ़ युद्ध का आदेश दिया गया है, सूरह अनफ़ाल में वर्णित है:
إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۔ ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍۢ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةًۭ فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ۔ (الانفال: ۵۵ تا ۵۸)
“अल्लाह की दृष्टि में धरती के जीवित प्राणियों में सबसे बुरे वे हैं, जिन्होंने अल्लाह का इंकार किया है और वे ईमान नहीं लाते। ये वे लोग हैं, जिनसे आपने संधि की, फिर वे प्रत्येक अवसर पर अपना वचन भंग कर देते हैं और (अल्लाह से) नहीं डरते। तो यदि ऐसे (वचनभंगी) आपको रणक्षेत्र में मिल जायें, तो उन्हें शिक्षाप्रद दण्ड दें, ताकि जो उनके पीछे हैं, वे शिक्षा ग्रहण करें। और यदि आपको किसी जाति से विश्वासघात (संधि भंग करने) का भय हो, तो बराबरी के आधार पर संधि तोड़ दें। क्योंकि अल्लाह विश्वासघातियों को पसन्द नहीं करता।” (अल-अनफ़ाल: 55-58)
इसी तरह, सुरह तौबा में, उन अवज्ञाकारियों के बारे में अधिक सख़्ती के साथ कहा गया है, जिन्होंने बार-बार मुसलमानों संधि की थी:
بَرَآءَةٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍۢ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ۔ (توبه : ۱-۲)
“यह अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन बहुदेववादियों के लिए बरी होने की घोषणा है, जिनसे आपने एक समझौता किया था (और जिन्होंने बार-बार इसका उल्लंघन किया था), अत: चार महीने, और ज़मीन पर चल फिर लो, इसके बाद अच्छी तरह से समझ लो कि तुम अल्लाह को विवश नहीं कर सकोगे और निश्चय अल्लाह, काफ़िरों को अपमानित करने वाला है।” (अत-तौबाः 1-2)
इसके बाद, उन बहुदेववादियों के बारे में जिन्होंने वचन नहीं तोड़ा था, आदेश दिया कि नियत समय तक उनके साथ की गई संधि का पालन करो। फिर दोबारा संधि तोड़ने वालों के बारे में कहा:
فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۢ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ۔ (توبه : ۵)
“जब सम्मानित महीने (जिसकी मोहलत दी गई है) बीत जायें, तो बहुदेववादियों को मारो, जहाँ कहीं पाओ और उन्हें पकड़ो और घेरो (ताकि वे मुसलमानों के बीच में न आ जाएँ) और उनकी घात में रहो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज़ की स्थापना करें तथा ज़कात दें, तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में, अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान् है।” (अत-तौबाः 5)
आगे चलकर फिर उन्हीं धोखेबाज़ और विश्वासघाती बहुदेववादियों के बारे में कहा:
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَـٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۔ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّۭا وَلَا ذِمَّةًۭ ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَـٰسِقُونَ۔ (التوبه : ۷-۸)
“इन बहुदेववादियों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के साथ अनुबंध कैसे हो सकता है, सिवाय उन लोगों के जिनके साथ तुमने प्रतिष्ठित मस्जिद (काबा) के पास समझौता किया था, जब तक वे अपने वचन पर जमे रहें, तुम भी जमे रहो, क्योंकि अल्लाह परहेज़गारों को पसंद करता है। लेकिन उन वचनभंग करने वालों की संधि कैसे रह सकती है, जबकि वे यदि तुमपर अधिकार पा जायें, तो किसी संधि और किसी वचन का पालन नहीं करेंगे। वे तुम्हें अपने मुखों से प्रसन्न करते हैं, जबकि उनके दिल इन्कार करते हैं (अर्थात्, वे अपने दिलों में तुम्हें क्षति पहुँचाने की चिन्ता में लगे रहते हैं) और उनमें अधिकांश दुष्ट और विद्रोही हैं।” (अत-तौबाः 7-8)
उसके बाद, फिर उन्हीं विश्वासघातियों के बारे में बताया:
لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّۭا وَلَا ذِمَّةًۭ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۔ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ۔ وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۔ أَلَا تُقَـٰتِلُونَ قَوْمًۭا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۔ قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ۔
(التوبه : ۱۰-۱۴ )
“वह किसी ईमान वाले के साथ किसी संधि और वचन का पालन नहीं करते और वही उल्लंघनकारी हैं। तो यदि वे (शिर्क से) तौबा कर लें, नमाज़ की स्थापना करें और ज़कात दें, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं और हम उन लोगों के लिए आयतों का वर्णन कर रहे हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं। तो यदि वे वचन देने के पश्चात अपनी क़समों को तोड़ दें और तुम्हारे धर्म पर हमले करें, तो कुफ़्र के लीडरों से युद्ध करो। क्योंकि उनकी क़समों का कोई विश्वास नहीं, ताकि वे (अत्याचार से) रुक जायेँ। तुम उन लोगों से युद्ध क्यों नहीं करते, जिन्होंने अपने वचन भंग कर दिये तथा रसूल को निकालने का निश्चय किया और उन्होंने ही पहले तुम पर हमला किया है? क्या तुम उनसे डरते हो? तो अल्लाह अधिक योग्य है कि तुम उससे डरो, यदि तुम ईमान वाले हो। उनसे युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे हाथों दण्ड देगा, उन्हें अपमानित करेगा, उनके विरुध्द तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वालों के दिलों का सब दुःख दूर करेगा।” (अत-तौबाः 10-14)
इन आयतों पर और उन हालात पर, जिनमें ये उतारी गईं, विचार करने से मालूम होता है कि:
1. जो लोग मुसलमानों के साथ संधि करने के बाद उसे तोड़ दें, तो उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसी में वे अवज्ञाकारी भी आते हैं जो मुसलमानों से आज्ञापालन का समझौता करते हैं और फिर इस्लामी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं।
2. उनके साथ कोई समझौता तो हो, लेकिन उनका रवैया इतना शत्रुतापूर्ण हो कि इस्लाम और मुसलमानों को हमेशा उनके द्वारा नुक़सान पहुँचाए जाने की आशंका बनी रहे तो उन्हें सार्वजनिक रूप से समझौते के रद्द होने की सूचना दे देनी चाहिए और उसके बाद उनकी दुश्मनी का जवाब देना चाहिए।
3. जो लोग बार-बार घोखेबाज़ी और विश्वासघात करें, और जिनके वादे और समझौते की कोई विश्वसनीयता न रहे, और जो मुसलमानों को क्षति पहुंचाने में नैतिकता और मानवता के किसी भी संविधान को न मानें, उनके ख़िलाफ़ शाश्वत युद्ध का आदेश दिया जाता है। केवल एक स्थिति में उनके साथ शांति हो सकती है कि वे तौबा करें और इस्लाम ले आएं। अन्यथा, इस्लाम और दारुल-इस्लाम को उनके प्रभाव से बचाने के लिए हत्या, गिरफ़्तारी, घेराबंदी और ऐसे अन्य उपाय करते रहना आवश्यक है।
(4) गुप्त आंतरिक शत्रु का दमन
इन बाहरी दुश्मनों के अलावा कुछ अंदरुनी दुश्मन भी हैं जो बाहर से तो दोस्त, लेकिन अंदर से इस्लाम की जड़ें काटने वाले होते हैं। ये लोग उस वर्ग में शामिल हैं जिसके लिए पवित्र क़ुरआन ने मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) का व्यापक शब्द इस्तेमाल किया है। और उनके बारे में यह आदेश दिया गया है:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ۔ (التوبہ: ۷۳)
“ऐ पैग़म्बर (सल्ल.), मुनाफ़िक़ों और अवज्ञाकारियों के ख़िलाफ़ जिहाद करो, और उनपर सख़्ती करो, उनका आवास नरक है और वह बहुत बुरा ठिकाना है।” (अत्तौबा: 73)
لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًۭا مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا۔ (الاحزاب: ۶۰-۶۱)
“यदि मुनाफ़िक तथा जिनके दिलों में रोग है और मदीना में अफ़्वाह फैलाने वाले, अपनी शत्रुता से बाज़ न आए, तो हम तुम को उन पर आच्छादित कर देंगे, । फिर वे इस नगर में तुम्हारे पड़ोसी बनकर नहीं रह सकेंगे सिवाय कुछ दिनों के। उन पर धिक्कार है। वे जहाँ पाये जायें, पकड़ लिए जाएंगे तथा जान से मार दिये जाएंगे।” (अल-अहज़ाब :60-61)
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا۔ (النساء: ٨٩)
“(हे ईमान वालो!) वे तो ये कामना करते हैं कि उन्हीं के समान तुमभी काफ़िर हो जाओ जिस तरह वे स्वयं काफ़िर हो गए, ताकि तुम और वे बराबर हो जाएँ। अतः तुम उनमें से किसी को अपना मित्र न बनाओ, जब तक कि वे अल्लाह की राह में अपने घरों को न निकलें। यदि वे इससे विमुख हों, तो उन्हें जहाँ पाओ, वध करो और उनमें से किसी को मित्र न बनाओ और न सहायक।” (अन्निसा: 89)
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا۔ (النساء: ۹۱)
“तथा तुम्हें कुछ ऐसे दूसरे लोग भी मिलेंगे, जो तुम्हारी ओर से भी शान्ति में रहना चाहते हैं और अपने समुदाय की ओर से भी शांति में रहना (चाहते हैं)। (इसलिए जब वे तुम्हारे पास आते हैं, तो वे इस्लाम को स्वीकार करते हैं) फिर जब षडयंत्र की ओर फेर दिये जायेँ, तो उसमें ओंधे होकर गिर जाते हैं। (यानी, वे स्वयं भी षडयंत्र में शामिल हो जाते हैं) तो यदि वे तुमसे विलग न हों और न तुमसे संधि करें और न तुम्हारे साथ युद्ध और शत्रुता से बाज़ आएं, तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ, उनकी हत्या करो। हमने उनके विरुध्द तुम्हें खुला तर्क दे दिया है।” (अल-निसा: 91)
इन आयतों में मुनाफ़िक़ों के इस समूह के अपराध का भी वर्णन किया गया है, जिसके कारण वे मारे जाने योग्य ठहरे। अधिक व्याख्या के लिए, हम पवित्र क़ुरआन की कुछ और आयतें प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि वे किस तरह के लोग हैं। सूरह निसा में है:
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ۔ (النساء : ۸۱)
“तथा वे (आपके सामने) कहते हैं कि हम आज्ञाकारी हैं और जब आपके पास से जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग, रात में, आपकी बात के विरुध्द साज़िश रचते हैं और जो साज़िश वे रच रहे हैं, उसे अल्लाह लिख रहा है।” (अन-निसा': 81)
सूरह तौबा में कहा:
لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًۭا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ . لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ ۔(التوبه : ۴۷-۴۸)
“अगर वे तुम्हारे साथ मिल कर युद्ध करने को निकलते, तो तुम्हारे भीतर उपद्रव के सिवा और कुछ न बढ़ाते, और झूठी बातें फैलाकर और लगाई-बुझाई करके तुम में बिगाड़ फैलाने का यत्न करते। और तुम में ऐसे भी लोग हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, और अल्लाह उन अत्याचारियों को भली-भाँति जानता है। वे इससे पहले (उहुद की लड़ाई में) विद्रोह करना चाहते थे, और आपके ख़िलाफ़ कई तरह के हथकंडे अपनाए थे, यहाँ तक कि सच्चाई की जीत हुई और अल्लाह का आदेश प्रबल हुआ, हालाँकि यह उनके लिए बहुत अप्रिय था।” (अत्तौबा :47-48)
وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌۭ يَفْرَقُونَ ٥٦ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَـٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًۭا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ (التوبه : ۵۷-۵۶)
“और वे (मुनाफ़िक़) अल्लाह की क़समें खाते हैं कि हम तुम में से हैं, हालाँकि वे तुम में से हैं ही नहीं, बल्कि वास्तव में कायर लोग हैं (जो तुम्हारी ताक़त देखकर दोस्ती जता रहे हैं)। अगर उन्हें कोई आश्रय या गुफा या छिपने की कोई जगह मिल जाए, तो उसकी ओर भागते हुए फिर जाएंगे।” (अत्तौबा :56-57)
ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ۔(التوبة: ٦٧)
“मुनाफ़िक़ पुरुष तथा मुनाफ़िक़ स्त्रियाँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे बुराई का आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बजाय अपने हाथ बंद किये रहते हैं। वे अल्लाह को भूल गये, तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया है। वास्तव में ये मुनाफ़िक़ बड़े ही दुष्कर्मी और अवज्ञाकारी हैं।” (अत्तौबा :67)
सूरह अल-अहज़ाब में कहा:
وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًۭا ۔ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌۭ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًۭا ۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَـَٔاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًۭا ۔ (الاحزاب: ۱۲-۱۴)
“और जब (जंगे अहज़ाब के मौक़े पर) मुनाफ़िक़ों ने और जिनके दिलों में शक का रोग है, कहने लगे, “अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था, वह झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं था।” और जब उनके एक समूह ने कहा, “ऐ यसरिब के लोगों, तुम्हारे लिए ठहरने का कोई अवसर नहीं है, यहाँ से भाग जाओ,” और उनमें से एक समूह नबी (सल्ल.) से अनुमति लेने लगा, यह कहते हुए कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वे खुले (असुरक्षित) नहीं थे और उनका मतलब भाग जाने के सिवा कुछ भी नहीं था। और यदि उनपर मदीने के चारों ओर से (सेनायें), प्रवेश कर जातीं फिर उनसे माँग की जाती (मुसलमानों की हत्या) के उपद्रव में शामिल हो जाओ, तो अवश्य उपद्रव कर देते और उसमें तनिक भी देर नहीं करते।”
सूरह अल-मुनाफ़िक़ुन में कहा:
إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُمْ جُنَّةًۭ فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۔(منافقون: ۱-۲)
“जब मुनाफ़िक़ तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि तुम बेशक ख़ुदा के रसूल हो। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ वाकई झूठे हैं। उन्होंने क़समों को (उनकी दुश्मनी के लिए) ढाल बना लिया है और वे अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और बहुत ही बुरा काम है, जो वे करते हैं।” (मुनाफ़िक़ून : 1-2)
ये आयतें बताती हैं कि कपटाचारियों का एक समूह ऐसा है जिसके साथ दिखावे के लिए भी मुसलमानों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इस समूह की विशेषता यह है कि या तो वह मुसलमान होने का दावा करने के बावजूद खुले आम कुफ़्र की बातें करता है, या अपनी ज़ुबान से तो इस्लाम क़ुबूल करता रहता है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वह हमेशा मुसलमानों की ताक में लगा रहता है। उनकी गुप्त ख़बरें दुश्मनों तक पहुंचाता है, और दुश्मनों के साथ मिलकर साज़िशें करता रहता है। उनके ईमान को ख़राब करने और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। उनकी मंडली में गड़बड़ी पैदा करके, मुसलमानों को विभाजित करता है। उनके दुश्मनों को नैतिक और व्यावहारिक समर्थन प्रदान करता है, और जब इस्लाम पर संकट का समय आता है, तो यह समूह उसे बचाने के बजाय उसे मिटाने की कोशिश करता है। यह समूह इस्लाम के लिए उसके बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए जो लोग इस ग़द्दार समूह से ताल्लुक़ रखते हों, भले ही वे हमेशा तौहीद और रिसालत की जाप करते हों और भले ही उसके इस्लामी दिखावे में किसी शक की कोई गुंजाइश न हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल कोई छूट नहीं देनी चाहिए। जब ऐसे लोगों से ये अपराध हों, तो इस्लाम के शरीर के इन फोड़ों पर सुधार के भाले का सख़्ती से उपयोग करना चाहिए।
(5) शांति की रक्षा
एक अन्य प्रकार के दुश्मन वे हैं जो दारुल-इस्लाम के अंदर रहते हैं या बाहर से आते हैं और उसमें बिगाड़ फैलाते हैं, डाके डालते हैं, हिंसा और हत्या करते हैं और इस्लामी राज्य की शांति और व्यवस्था को बाधित करते हैं, या हिंसा के माध्यम से इस्लामी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। उनके संबंध में पवित्र क़ुरआन में यह आदेश दिया गया है:
إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَـٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ۔ (المائده: ۳۳-۳۴)
“जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और देश में (लूटपाट करके) उत्पात फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा यह है कि उन्हें मार डाला जाए, या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ-पैर विपरीत दिशा में काट दिए जाएं, या उन्हें देश से निकाल दिया जाए। यह दुनिया में उनके लिए अपमान है, और (इसके अलावा) उनके लिए आख़िरत में एक बड़ी सज़ा है। सिवाय उनके जो तौबा कर लें, इससे पहले कि उन पर तुम्हारा अधिकार हो (अर्थात् उन्हें गिरफ़्तार कर लो), तो जान लो कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है।” (अल-मायदा: 33-34)
जिस मौक़े पर यह आयत नाज़िल हुई, उससे पता चलता है कि इसका आदेश विद्रोहियों और शांति व्यवस्था के ख़िलाफ़ हथियारबंद उपद्रव के लिए है। हज़रत अनस बिन मलिक से रिवायत है कि उरैना क़बीले के कुछ लोग रसूल (सल्ल.) की ख़िदमत में आए, फिर मुसलमान हो गए और मदीना में रहने लगे, लेकिन वहां का वातावरण उन्हें रास नहीं आया और वे बीमार पड़ गए। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उनसे कहा कि, अगर तुम हमारे ऊँटों के बीच जाकर रहो और उनका दूध पियो और उनका पेशाब दवा के रूप में लो! तो तुम्हारी सेहत में सुधार आएगा। अतः वे मदीना के बाहर ऊँटों के चरागाहों में पहुँचे और जब वे ठीक हो चुके तो इस्लाम से विमुख हो गए। अल्लाह के रसूल के चरवाहों को मार डाला और ऊँटों को भगा ले गए। उनकी इस हरकत की ख़बर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को मिली, तो आपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। जब वे गिरफ़्तार कर लाए गए तो आप ने सज़ा-ए मौत दिलवाई। पवित्र क़ुरआन में निर्धारित ये दंड उन लोगों के लिए हैं जो दारुल-इस्लाम में लूटपाट और हत्या करके शांति को भंग करते हैं। अलग-अलग डिग्री की सज़ा अपराध की अलग-अलग डिग्री से संबंधित है जो न्यायविदों ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है।
(6) कमज़ोरों और दमितों की सहायता
रक्षात्मक युद्ध का एक और रूप जिसमें मुसलमानों को तलवार उठाने की अनुमति दी गई है, यह है कि अगर मुसलमानों का एक दल अपनी कमज़ोरी और शक्ति की कमी के कारण दुश्मनों के चंगुल में फंस जाए और उसके पास ख़ुद को मुक्त करने के लिए पर्याप्त ताक़त न हो। ऐसी स्थिति में अन्य मुसलमान जो स्वतंत्र हैं और युद्ध की शक्ति रखते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने उत्पीड़ित भाइयों को इस उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए लड़ें। क़ुरआन में कहा गया है:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا○ (النساء:۷۵)
“और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में उन कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध नहीं करते हो, जो कहते हैं, “ऐ हमारे रब! हमें इस बस्ती से निकाल, जहाँ के लोग बड़े ज़ालिम हैं और हमारे लिए अपनी ओर से किसी को समर्थक और अपनी ओर से किसी को सहायक बना।” (अल-निसा : 75)
दूसरी जगह, इस सहायता की ज़रूरत को स्पष्ट रूप से बताया गया है और इस पर ज़ोर दिया गया है:
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ ○ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌۭ كَبِيرٌۭ○ (الانفال : ۷۲-۷۳)
“जो लोग ईमान तो लाए, लेकिन दारुल-कुफ़्र को छोड़ कर दारुल-इस्लाम में नहीं आए, उनसे तुम्हारी सहायता का कोई संबंध नहीं, जब तक कि वे प्रवास नहीं करते। हालांकि, अगर वे तुम से धर्म के मामलों में मदद मांगते हैं, तो यह है तुम पर उनकी मदद करना अनिवार्य है, सिवाय इसके कि जब वे उस समुदाय के ख़िलाफ़ मदद मांगें, जिसके साथ तुम्हारी संधि है। जो कुछ भी तुम करते हो, अल्लाह उसे अच्छी तरह देखता है। इनकार करने वाले लोग एक दूसरे के संरक्षक और सहायक हैं। इसलिए अगर तुम (मुसलमानों की मदद) न करोगे तो देश में फ़ितना फैलेगा और बड़ी तबाही होगी।” (अल-अनफ़ाल: 72-73)
इस आयत में आज़ाद मुसलमानों और ग़ुलाम मुसलमानों के बीच के रिश्ते को बहुत ही स्पष्ट रूप से बयान किया गया है। पहले, यह कहा गया है कि जो मुसलमान दारुल-कुफ़्र में रहना स्वीकार करें या रहने के लिए मजबूर हों, वे दारुल-इस्लाम के मुसलमानों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध नहीं रख सकते हैं। अर्थात वे आपस में शादी-विवाह के सम्बंध स्थापित नहीं कर सकते, न ही वे एक-दूसरे की विरासत प्राप्त कर सकते हैं, न ही ‘फ़य’ (इस्लामी राज्य को सैन्य कार्रवाई के बिना प्राप्त होने वाला धन) और ‘ग़नीमत’ (इस्लामी राज्य को युद्ध जीतने पर प्राप्त शत्रु सेना का माल) में उनका कोई हिस्सा हो सकता है, न ही वे सदक़ा ले सकते हैं, और न ही इस्लामी राज्य में उन्हें कोई पद दिया जा सकता है, जब तक कि वे दारुल-कुफ़्र से पलायन करके दारुल-इस्लाम के नागरिक नहीं बन जाते। लेकिन इन सभी बंधनों को काट देने के बावजूद, एक रिश्ता, समर्थन और मदद का रिश्ता फिर भी नहीं काटा गया। और क़ुरआन से साफ़ कर दिया कि ‘नुसरत’ (सहयोग और समर्थन) का संबंध दीन के साथ जुड़ा है। जब तक कोई व्यक्ति मुसलमान है, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, उसके साथ मुसलमानों का सहयोग और समर्थन का संबंध किसी भी सूरत में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर उसके दीन को कोई ख़तरा हो या उस पर ज़ुल्म हुआ हो और वह अपने दीनी रिश्ते का वास्ता देकर मदद मांगे तो मुसलमानों पर उसकी मदद करना अनिवार्य है, शर्त यह है कि जिसके ख़िलाफ़ मदद मांगी गई है, उससे मुसलमानों का समझौता न हो, क्योंकि समझौते की स्थिति में मुसलमानों के लिए अपने मुस्लिम भाई की मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी है क़रार निभाना। अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पहले उनकी मदद करना उनके लिए जायज़ नहीं है। इस आदेश को बताने के बाद मदद और समर्थन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है और कहा है कि देखिए ये अवज्ञाकारी किस तरह इस्लाम को मिटाने में एक दूसरे की मदद करते हैं और किस तरह आपसी विरोध और दुश्मनी के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हो जाते हैं। अत: अगर तुम भी दीनी सम्बन्धों को ध्यान में रखकर एक-दूसरे के सहायक न बनो, तो ज़मीन में फ़ितना फैल जाए? फ़ितना शब्द, जैसा कि हम बाद में स्पष्ट करेंगे, क़ुरआन की शब्दावली में अधर्मिता के प्रभुत्व और सत्य धर्म के अनुयायियों को पीड़ित और अपमानित होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह, फ़साद भी मार्गदर्शन पर गुमराही की प्रधानता और भलाई के मिट जाने के अर्थ में बोला जाता है। इसलिए, अल्लाह तआला मुसलमानों के एक समूह को मिटाने या सही रास्ते से भटकाने की व्याख्या फ़ितना और फ़साद के रूप में करता है, और इस फ़ित्ना से लड़ना मुसलमानों का दायित्व ठहराता है।
रक्षा का उद्देश्य:
अब अगर आप रक्षात्मक युद्ध के उन सभी रूपों पर एक नज़र डालें जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि उन सभी में एक ही उद्देश्य काम कर रहा है, और वह यह है कि मुसलमान अपने धर्म और अपने राष्ट्रीय अस्तित्व किसी भी स्थिति में बुराई और दुष्टता से अभिभूत न होने दें। बुराई बाहर से आए, या अंदर से, उसका सिर कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहें। अल्लाह को मुसलमानों से जो काम लेना है, उसके लिए पहली ज़रूरत यह है कि ये बिगाड़ और षडयंत्रों से सुरक्षित रहें और इनकी राष्ट्रीय और राजनीतिक शक्ति मज़बूत बनी रहे। अगर वे अपने आप को मिटने से नहीं बचाते हैं और आंतरिक और बाहरी शत्रुओं के षडयंत्रों की उपेक्षा करते हैं और ख़ुद को उन सामूहिक बीमारियों का शिकार होने देते हैं जिन्होंने अतीत की अत्याचारी क़ौमों को अपमान, असफलता और अल्लाह के प्रकोप का भागी बनाया, तो ज़ाहिर है कि वे केवल अपने आप को ही मुसीबत में न डालेंगे, बल्कि वे मानवता की उस महान सेवा को करने में भी सक्षम नहीं होंगे जिसके लिए उन्हें खड़ा किया गया है। उनका यह अत्याचार केवल अपने अप पर ही नहीं होगा, बल्कि पूरे मानव जगत पर अत्याचार होगा। इसलिए उन्हें खोल-खोल कर और बड़ी स्पष्टता के साथ उन दुश्मनों के संकेत बताए गए हैं जो उनके विनाश का कारण बन सकते हैं और एक-एक का धर तोड़ देने का आदेश दिया गया है, ताकि वे मार्गदर्शन के प्रकाश को मिटाने और सार्वभौमिक सुधार के कार्य के मार्ग में रुकावट बनने के योग्य न रहें। इसके सिए केवल तब तलवार उठाने का निर्देश नहीं दिया गया, जब बुराई अपना सिर उठाए और उत्पात मचाने लगे, बल्कि उससे यह आग्रह किया गया कि वह हर समय उसका सामना करने के लिए तैयार रहे, ताकि वह अपना सिर निकालने का साहस ही न कर सके और उस पर सत्य का इतना डर बैठा रहे कि उसका दम अंदर ही अंदर घुट जाए।
وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍۢ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍۢ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ○َ (الاانفال:۶۰)
“उनके मुक़ाबले के लिए जितना हो सके, युद्ध के उपकरण और घोड़े तैयार रखो। इससे तुम अल्लाह के शत्रुओं और अपने शत्रुओं और उनके सिवा उन लोगों को जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह उन्हें जानता है, भयभीत करोगे। तुम अल्लाह के मार्ग में जो कुछ भी ख़र्च करोगे, वह तुम्हें दुनिया में शांति, समृद्धि और इस्लाम के विकास के रूप में और अल्लाह की ख़ुशी के रूप में) पूरे का पूरा वापस मिल जाएगा और तुम पर बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया जाएगा।” (अल-अनफ़ाल:60)
यह आयत इंगित करती है कि मुसलमानों की युद्ध ज़रूरतों के लिए उस प्रकार की अस्थायी सेना (मिलिशिया) पर्याप्त नहीं हो सकती है, जो किसी विशेष ज़रूरत के अवसर पर एकत्र की जाती है और ज़रूरत समाप्त होने के बाद तितर-बितर हो जाती है, बल्कि उन्हें एक स्थायी सेना (स्टैंडिंग आर्मी) रखनी चाहिए, जो सदैव कील-काँटों से लैस रहे। आयत में युद्ध उपकरणों की प्रकृति का वर्णन केवल “क़ुव्वह” (शक्ति) शब्द से किया गया है। जिसमें पहली शताब्दी हिजरी के तीर-धनुषों, चौदहवीं शताब्दी के बंदूक़ों, तोपों, हवाई जहाज़ और पनडुब्बियों से लेकर अगली शताब्दियों के सर्वश्रेष्ठ सामरिक हथियारों तक सब कुछ शामिल है। “मस्ततअतुम” (जितनी तुम्हारी क्षमता हो) शब्द ने शक्ति की तीव्रता को मुसलमानों की क्षमता से जोड़ दिया। अर्थात अगर उनके पास एक बड़ी सेना प्रदान करने की शक्ति है, तो उन्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है और वे बड़े, बड़े युद्धपोत, बड़े घातक हथियार प्राप्त न कर सकें, तो उनपर से यह दायित्व रद्द नहीं कर दिया जाता, बल्कि उन्हें युद्ध के हर उस तरीक़े को अपनाना चाहिए जिसका इस्तेमाल सच्चाई के दुश्मनों से लड़ने के लिए किया जा सकता है और जिसे हासिल करना मुसलमानों के लिए संभव है। फिर पले हुए घोड़े को तैयार रखने की समीचीनता को समझाते हुए, ‘अल्लाह के और अपने शत्रुओं को भयभीत करने के लिए’, के साथ ‘और उनके सिवा उन लोगों को जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह उन्हें जानता है’ जो कहा गया उसमें राजनीति के इस बिंदु को समझाया गया है कि अगर एक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति को मज़बूत रखता है, तो उससे केवल यही लाभ नहीं होता है कि उसकी खुली दुश्मन शक्तियाँ उससे भयभीत रहती हैं, बल्कि धीरे-धीरे उसकी ऐसी धाक जम जाती है कि उससे दुश्मनी करने का विचार भी किसी के मन में नहीं आता। वे विद्रोही शक्तियाँ जो उसे कमज़ोर और बेपरवाह देखकर उस पर आक्रमण करने से तनिक नहीं हिचकिचातीं, उसके प्रति इतनी आज्ञाकारी और मैत्रीपूर्ण बनी रहती हैं कि उनके स्वभाव में छिपे विद्रोह का पता ही नहीं चलता। उसके बाद अर्थशास्त्र के तथ्य को समझाया गया है कि यह मत समझो कि इस परिरक्षण की तैयारी में ख़र्च की गई राशि हमेशा के लिए खो जाती है, और आप उसके लाभों से वंचित हो जाते हैं बल्कि वास्तव में यह तुम्हारे पास वापस आ जाता है। इस तरह से कि तुम पर अत्याचार नहीं हो सकता है, और अगर तुम अत्याचार से सुरक्षित हो, तो तुम्हें शांतिपूर्ण जीवन का लाभ मिलता है। “और तुम पर बिल्कुल भी अन्याय नहीं किया जाएगा” में इस दुनिया और आख़िरत दोनों के लाभ प्राप्त होने और दोनों में अत्याचार से बचे रहने का वादा निहित है। वास्तव में इस वाक्य से दोनों आशयित हैं, क्योंकि मुसलमानों के परलोक की भलाई वही है, जो उनकी दुनिया की भलाई है और उनकी दुनिया की गिरावट वही है, जिसका परिणाम परलोक का घाटा है।
तीसरा अध्याय : सुधार के लिए युद्ध
अब विचार किया जाना चाहिए कि रक्षात्मक युद्ध के इन आदेशों से मुसलमानों की जिस राष्ट्रीय शक्ति को नष्ट होने से बचाया गया है, उसका उपयोग क्या है। क्या इस शक्ति को बचाना ही मुख्य उद्देश्य है, या इससे कुछ और काम लेना है, जिसके लिए इसे फ़ितनों से बचाना आवश्यक है? पिछले पृष्ठों में हमने बार-बार इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि मुसलमान, अपनी राष्ट्रीय ताक़त खोकर, “मूल सेवा” के योग्य नहीं रह सकते, जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया है, तो इससे हमारा उद्देश्य वास्तव में, इसी प्रश्न का उत्तर देना था।
क़ुरआन, एक व्यापक किताब है, जिसमें इस्लामी शिक्षण के हर पहलू का विवरण है। वह यह वर्णन भी करता है कि मुसलमानों को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और “मूल सेवा” की व्याख्या भी करता है, जिस के लिए उनकी शक्ति की रक्षा के लिए यह सब व्यवस्था की गई है। वह कहता है:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ○ (آل عمران:۱۱۰)
“तुम, सबसे अच्छी उम्मत (समुदाय) हो, जिसे सब लोगों के लिए निकाला गया है कि तुम भलाई का आदेश देते हो तथा बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान (विश्वास) रखते हो।” (आले-इमरान: 110)
इस कथन में, यह नहीं कहा गया है कि 'अरबों के लिए निकाला गया’ या 'पूर्व के लिए निकाला गया’ या 'पश्चिम के लिए निकाला गया’ बल्कि, यह कहा गया है कि समस्त मानव जाति की सेवा के लिए निकाला गया और वह सेवा है, भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना।
एक सनुदाय के जीवन का उद्देश्य समस्त मानव जाति की सेवा करना, यह कुछ ऐसी अवधारणा है जिससे राष्ट्रवाद और देशभक्ति के माहौल में पले-बढ़े संकीर्ण दिमाग़ परिचित नहीं हैं। वे “साम्प्रदायिकता” और “देशप्रेम” को तो ख़ूब जानते हैं और “राष्ट्रवाद” तो मानो उनकी सोच की प्राकाष्ठा है, लेकिन भौगोलिक और जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर, संपूर्ण मानव जगत के लिए व्यावहारिक सेवा करना और इसे संपूर्ण राष्ट्र का जीवन-लक्ष्य ठहराना उनकी सोच से बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले हमें इसकी व्याख्या करनी चाहिए कि ‘उख़रिजत लिन्नास’ (समस्त मानव जाति के लिए निकाला गया) क्या चीज़ है।
सामुदायिक दायित्व की नैतिक अवधारणा
अगर मनुष्य की सहज इच्छाओं का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से उसमें कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो निम्नतम स्तर के जीवों में भी मौजूद नहीं हो। जैसे मनुष्य अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, वैसे ही घोड़ा भी अच्छी हरी घास खाना चाहता है। जिस तरह एक आदमी दूसरे आदमियों पर प्रभुत्व पाकर खुश होता है, उसी तरह एक मेढ़े के खुश होने का इससे बड़ा अवसर कोई नहीं होता है कि कोई मेढ़ा उसकी टक्कर का सामना न कर सके। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षात्मक उपाय करता है, उसी तरह यह गुण एक छोटे से छोटे कीट में भी पाया जाता है। इसलिए, अमूर्त इच्छाओं के संदर्भ में मनुष्य और पशु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जो चीज़ इसे तुच्छ जीवों से अलग करती है, वह यह है कि पशु जीवन का अंतिम उद्देश्य इन इच्छाओं को पूरा करना है, नगर मानव जीवन का उद्देश्य इन इच्छाओं की पूर्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह एक उच्चतम लक्ष्य के लिए, एक माध्यम के रूप में उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। अगर मनुष्य के पास वास्तव में अपने पाशविक लक्ष्यों से ऊँचा कोई मानवीय लक्ष्य न हो और वह अपनी बुद्धि और उस विवेक को जो अल्लाह ने उसे दिया है, केवल ऐसे साधनों और तरीक़ों को खोजने में ख़र्च करे जिनसे वह अपनी पाशविक इच्छाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, तो वह निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का पशु तो बन सकता है, लेकिन एक उच्च कोटि का मनुष्य नहीं बन सकता।
मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए रोज़ी-रोटी कमाने को विवश है, नहीं तो वह भूखा मर जाएगा। शारीरिक विकारों से सुरक्षित रहने के लिए उसे घर बनाने, कपड़े पहनने और सुरक्षा के अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए विवश होना पड़ता है, अन्यथा वह जीवित न रह पाएगा। और इसी तरह वह दुश्मनों से ख़ुद को बचाने के लिए भी मजबूर हो जाता है। लेकिन इन ज़रूरतों को पूरा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। तो सच्चा मनुष्य वह है जो अपने निजी अधिकारों की पूर्ति केवल इस लिए करता है, कि वह अपने परिवार, अपने शहर, अपने समुदाय, अपने देश, और अपने जैसे दूसरे मनुष्यो और अपने अल्लाह के अधिकारों को पूरा करने में सक्षम हो सके। उन दायित्वों को बेहतर तरीक़े से पूरा कर सके जो सर्वजगत के रचयिता और पालनहार द्वारा उसे सौंपा गया है। मानवता का वास्तविक मानक इन अधिकारों और दायित्वों को अच्छी तरह समझना और इन्हें पूरा करना है। मनुष्य को अपने निजी अधिकारों की पूर्ति का दायित्व इस लिए सौंपा गया है, कि उसके ज़िम्मे केवल उसके अपने अधिकार नहीं हैं, बल्कि वह दूसरों के अधिकारों के लिए भी ज़िम्मेदार है। अगर वह अपने अधिकार की पूर्ति नहीं करता है तो वह दूसरों के अधिकारों की पूर्ति भी नहीं कर पाएगा।
जब व्यक्तियों के लिए मानवता का यह मानक सही है, तो कोई कारण नहीं है कि वही मानक समुदायों के लिए सही न हो। संगठन बन जाने से मनुष्यता में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो जाती। इसलिए, मानव जाति के सामूहिक प्रतिष्ठा का मानक भी वही होना चाहिए जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का है। अगर किसी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल आत्म-साधना और स्वयं-सेवा के सिवा कुछ न हो, तो वह हमारी दृष्टि में एक विवेकशील पशु से अधिक मूल्य नहीं पा सकता, तो निश्चय ही एक ऐसा मानव समाज भी सभ्य पशुओं से अधिक मूल्य का पात्र नहीं, जिसके प्रयासों का दायरा केवल अपने कल्याण, विकास और अपनी शांति और समृद्धि तक ही सीमित हो और सामान्य मानव कल्याण से उसे कोई मतलब न हो। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की आग बुझाने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने जीवन और संपत्ति और सम्मान की रक्षा करने में तो बहुत सक्रिय हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के घर को जलता देखकर दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन और दूसरे व्यक्ति के धन और सम्मान और प्रतिष्ठा को नष्ट होते हुए देख कर टस से मस न हो, तो उसे एक अच्छा आदमी तो दूर “आदमी” कहने में भी संकोच होगा। इसी तरह एक ऐसे समुदाय को हम सभ्य कैसे कह सकते हैं जो ख़ुद को बचाने, ख़ुद से बुराई को दूर करने और अपने घर को बचाने के लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, मगर जब अन्य समुदायों पर बुराई का प्रभुत्व हो, अनिष्ट शक्तियों के विद्रोह से अन्य राष्ट्रों का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो रहा हो, तो वह उनके उद्धार, उनकी स्वतंत्रता और उनके कल्याण के लिए प्रयास करने से इंकार कर दे। जिस प्रकार व्यक्तियों पर केवल निजी ही नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे इनसानों और अपने अल्लाह के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिन्हें पूरा करना उनका दायित्व होता है, उसी तरह, एक समुदाय के ऊपर भी व्यापक मानव समुदाय और उसके निर्माता के कुछ अधिकार होते हैं और यह कभी भी एक सभ्य समुदाय कहलाने के योग्य नहीं हो सकता जब तक कि वह उन अधिकारों को पूरा करने में अपने तन,मन और धन से जिहाद न करे। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, अपने अस्तित्व को बनाए रखना और बुराई के प्रभुत्व से अपनी रक्षा करना निश्चित रूप से एक राष्ट्र का पहला दायित्व है। लेकिन केवल यही एकमात्र दायित्व नहीं है जिसे पूरा करके उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक दायित्व यह है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग समस्त मानव जाति को बचाने के लिए करे, मानवता के मार्ग से उन सभी बाधाओं को दूर करे, जो उसके नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालते हैं, और जब तक दुनिया में बुरी ताक़तें हैं, तब तक वह उन के दमन के लिए लड़ना जारी रखे।
सामुदायिक दायित्व से जुड़ी इस्लाम की उच्च शिक्षा
यह बहुत दुखद है कि दुनिया के संकीर्ण सोच वाले ज्ञानियों ने सामूहिक प्रतिष्ठा के इस उच्च स्तर और सामूहिक जीवन के इस उच्च आदर्श को समझने की कोशिश नहीं की। अगर किसी ने कोशिश की भी, तो उसकी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं पहुँच सकी। ये लोग जब व्यक्तियों के नैतिक दायित्वों की चर्चा करते हैं, तो मानवता की वृहद अवधारणा के लिए उनकी सोच सिकुड़ जाती है और सामूहिक दायित्वों को राष्ट्रीयता के सीमित दायरे में समेट कर वे उस राष्ट्रवाद या देशभक्ति की नींव रखते हैं, जो थोड़े से बदलाव के बाद आसानी से साम्प्रदायिक भेदभाव का रूप ले लेता है। यह संकीर्णता ही वास्तव में मानवता के इस अप्राकृतिक विभाजन की ज़िम्मेदार है, जिसके कारण एक जाति या एक भाषा या एक राष्ट्रीयता के लोग अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों को सार्वभौमिक मानवता से बाहर मानते हैं, और उनके अधिकारों को समझना और पूरा करना तो दूर, उनका हनन करने और उन्हें कुचलने को भी नैतिकता और शालीनता के ख़िलाफ़ नहीं मानते।
पवित्र क़ुरआन ने अपने कथन ‘उख़रिजत लिन्नास’ (समस्त मानव जाति के लिए निकाला गया) से वास्तव में मानवता के इस अभौतिक और अस्वभाविक विभाजन को रद्द कर दिया है। इसने सामूहिक शालीनता के इस उच्च मानक को पेश करके मुस्लिम समुदाय को सार्वभौमिक मानव सेवा के इस उच्च आदर्श की ओर निर्देशित किया है जो सभी प्रकार के भेदों से ऊपर है। उसका कहना है कि एक सत्यभक्त समुदाय के दायित्व के लिए राष्ट्रीयता का क्षेत्र बहुत संकीर्ण है, यह एक जाति या एक भाषा या एक देश की क़ैद को सहन नहीं कर सकता है, इसके लिए भूमि और जल और दिशाओं और आयामों की सीमाएं भी अर्थहीन हैं। एशिया और यूरोप या पूर्व और पश्चिम के बीच का भेद उसे अपने दायित्व को पूरा करने में बाधा नहीं बन सकता है। उसके अनुसार, सभी मनुष्य और आदम के सभी बेटे और बेटियाँ समान हैं। उन सभी की सेवा करना, अर्थात् उन सभी को भलाई का आदेश देना, बुराई से रोकना और उन्हें बिगाड़ से बचाना उसका दायित्व है। इस उच्च शिक्षा को क़ुरआन ने विभिन्न प्रभावी रूपों में प्रस्तुत किया है और संकीर्णता के बंधन को तोड़कर दायित्व निर्वहन की एक व्यापक दुनिया का रास्ता खोल दिया है। अतः एक अन्य स्थान पर कहा गया है:
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةًۭ وَسَطًۭا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًۭا ۗ○(البقرہ :۱۴۳)
“इस प्रकार हमने तुम्हें एक उच्च और सम्मानित समुदाय बनाया है, ताकि तुम संसार के लोगों पर (सच्चाई के) साक्षी रहो और रसूल तुम्हारे ऊपर साक्षी हो।” (अल-बक़रह: 143)
सूरह हज में इसी लेख की व्याख्या इस प्रकार की गई है:
وَجَـٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ ○ (الحج: ۷۸)
“और अल्लाह के मार्ग में ऐसा जिहाद करो, जैसा जिहाद करना अपेक्षित है, उसने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है और दीन (धर्म) के दायरे में तुम्हें प्रतिबंधित नहीं किया है। यह वही समुदाय है कि तुम्हारे पिता इब्राहीम, का था। अल्लाह ने तुम्हारा नाम इससे पहले भी और इस किताब में भी मुस्लिम (आज्ञाकारी) रखा है, ताकि रसूल तुम पर गवाह हों और तुम दुनिया वालों पर गवाह हो। अतः नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो और अल्लाह की राह पर दृढ़ता के साथ जमे रहो।” (अल-हज:78)
एक दूसरे की व्याख्या करने वाली इन दोनों आयतों को मिला कर पढ़ें तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि यहां भी मुसलमानों के जीवन का उद्देश्य मानव जाति की सेवा ही बताया गया है। कहा गया कि तुम एक उत्कृष्ट समूह हो जो अतिवाद से हटकर न्याय और संयम के मार्ग पर स्थापित हुए हो। अल्लाह ने तुमको विशेष रूप से इस काम के लिए चुना है, कि अपने कथन और कर्म से सत्य की गवाही दो, और दुनिया में सच्चाई के गवाह बनकर रहो, ताकि जीवन के हर पहलू में तुम्हारे कथन और तुम्हारे व्यवहार से दुनिया जान सके कि सत्य क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय का क्या अर्थ है और अच्छाई किसी चीज़ का नाम है। सत्य की यही गवाही तुम्हारे जीवन का मक़सद है और इसी के लिए तुम्हें मुस्लिम (अल्लाह के आज्ञाकारी समुदाय) का नाम दिया गया है। इसके बाद कहा गया कि तुम्हारे इस दीन में कोई संकीर्णता नहीं है, बल्कि इसका दायरा इतना विस्तृत रखा गया है कि जाति, रंग, भाषा, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सीमाएँ उसकी उपयोगिता को आम होने से नहीं रोक सकतीं। इसमें कोई छुआ-छूत या वर्णाश्रम की शर्त नहीं है, न इसराईल की खोई हुई भेड़ों या इस्माईल के भटके हुए ऊंटों का कोई विनियोग है। हर वह इंसान, जो इस्लाम के सिद्धांतों को स्वीकार करे चाहे किसी नस्ल और राष्ट्र का हो और किसी देश का निवासी हो, तुम्हारे इस दीन में समान रूप से शामिल हो सकता है। इसी तरह, तुम को सौंपी गई सेवा का दायरा किसी एक देश या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम को पूरी मानवता के लिए सत्य का साक्षी बन कर रहना है।
फिर एक दूसरे तरीक़े से उसी विषय को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है:
ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ○ (الحج: ۴۱)
“ये वो लोग हैं जो अगर हम उन्हें ज़मीन में ताक़त दें तो नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।” (अल-हज: 41)
यहाँ 'अल-अर्ज' शब्द का प्रयोग किया गया है और मुसलमानों की ताक़त का फ़ायदा यह बताया गया है कि वे ज़मीन में ख़ुदा की इबादत को बढ़ावा देंगे, अच्छे कामों का प्रसार करेंगे और बुराई को मिटाएंगे। इसका मतलब भी यह बताना है कि मुसलमानों का काम केवल अरबों के लिए है या केवल एशिया के लिए या केवल पूर्व के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। उन्हें ज़मीन के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। उन्हें ज़मीन के हर मैदान और पहाड़ और समुद्र में अच्छाई का झंडा लिए हुए बुराई की सेनाओं का पीछा करना चाहिए, और अगर दुनिया में एक कोना भी ऐसा बच गया, जहां बुराई मौजूद हो, तो वहाँ पहुँचकर उसे मिटा देना चाहिए और भलाई (अच्छाई) को उसके स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। अल्लाह का किसी देश विशेष या किसी जाति विशेष से संबंध नहीं है। वह अपनी समस्त सृष्टि का समान रूप से निर्माता है और सब से बराबर संबंध रखता है। इसलिए धरती में कहीं भी बुराई और बिगाड़ का होना, उसके लिए समान रूप से नाराज़गी का कारण बनता है। पवित्र क़ुरआन में, ‘अरब में बिगाड़’ या ‘अजम (ग़ैर-अरब) में बिगाड़’ कहीं नहीं आया है, हर जगह ‘ज़मीन’ के शब्द का उपयोग किया गया है। वह अपनी सेना, यानी मुस्लिम उम्मत (समुदाय) की सेवा को राष्ट्रीयता या जाति की सीमाओं में सीमित नहीं करता है, बल्कि इस दया को ज़मीन के सभी निवासियों तक पहुंचाता है।
‘भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने’ की वास्तविकता
इससे ज्ञात हुआ कि मुसलमानों के सर्वश्रेष्ठ समुदाय होने का कारण यह है कि वे केवल अपनी सेवा के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि उनके अस्तित्व का उद्देश्य पूरी मानवता की सेवा करना है। उनकी श्रेष्ठता का रहस्य ‘उख़रिजत लिन्नास’ (समस्त मानव जाति के लिए निकाला गया) में छिपा है। उन्हें राष्ट्रवाद या देशभक्ति के लिए नहीं उठाया गया है, बल्कि यह इस्लाम की प्रकृति की मांग है कि वे मानवता के सेवक बन कर रहें।
अब यह देखना चाहिए कि मुसलमानों की वास्तविक सेवा जो “अम्र बिल-मारूफ़ व नह्यि अनिल-मुनकर” (मारूफ़ {भलाई} का आदेश देना और मुनकर {बुराई} से रोकना) के व्यापक शब्दों में वर्णित है, यह किस प्रकार की सेवा है और इसकी वास्तविकता क्या है।
“मारूफ़” शब्दकोश में उसे कहते हैं जो जानी-पहचानी हो, और इस शब्द से इसका मतलब हर उस कार्य से है, जिससे बुद्धि परिचित हो, जिसके गुणों को मानव-प्रकृति जानती और समझती हो, और जिसे देखकर हर आदमी का दिल गवाही दे कि यह वास्तव में अच्छाई है। इसके विपरीत, “मुनकर” शब्द है जो अरबी शब्दकोष में अज्ञात और अपरिचित चीज़ के लिए बोला जाता है और यह शब्द उस क्रिया पर लागू होता है जिसे मानव-प्रकृति पसंद न करती हो और बुद्धि उसे बुराई समझती हो, और आम आदमी जिसे अवांछनीय मानते हों। ईमानदारी, सच्चाई, धर्मपरायणता, दायित्व की भावना, कमज़ोरों का समर्थन, पीड़ितों के लिए दया, शोषितों की मदद करना, न्याय स्थापित करना, अल्लाह और बन्दों और स्वयं के अधिकारों को समझना और पूरा करना, ये और ऐसे अन्य नैतिकत गुण “मारूफ़” हैं। और उन पर अमल करने और दूसरों को प्रोत्साहित करने के कार्य को “अम्र बिल-मारूफ़” कहा जाता है। इसके विपरीत, झूठ, धोखा, विश्वासघात, षडयंत्र, बिगाड़, सच्चाई और धार्मिकता को दबाना, कमज़ोरों को सताना, ये और ऐसे ही अन्य मानवताविरोधी, अतार्किक और प्रकृति के ख़िलाफ़ ऐसे सभी कार्य “मुनकर” हैं और उनसे ख़ुद बचना और दूसरों को रोकना “नह्यि अनिल-मुनकर” है।
इसमें ख़ुद नेकी करने और बुराई से परहेज़ करने को प्राथमिकता दी गई है, और नेक बनाने और बुराई से रोकने को दूसरा स्थान दिया गया है। सच भी यही है कि अच्छा बनाने से पहले अच्छा बनना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह अपना पेट भरने से दूसरों का पेट भरना बेहतर है, उसी तरह अच्छाई को फैलाने और बुराई को रोकने का स्तर भी अच्छाई अपनाने और बुराई को त्यागने से ऊंचा है। क्योंकि एक स्वयं की सेवा है, और दूसरी अपने भाइयों की सेवा है। एक मात्र मानवता की श्रेणी में है और दूसरा पूर्ण मानवता की श्रेणी में है। अच्छाई का अभ्यास करना और बुराई से बचना निश्चित रूप से सज्जन व्यक्ति का एक अच्छा गुण है, लेकिन सज्जनता की पूर्णता और प्रतिष्ठा का सर्वोच्च पद तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह दूसरों को भी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करने और बुरे कर्मों से बचाने की कोशिश न करे।
इंसान का स्वभाव होता है कि अगर उसे कोई चीज़ अप्रिय लगती है तो वह उसे छोड़ देता है। अगर अप्रियता घृणा के स्तर पर पहुंच जाए तो उसे देखना या सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर घृणा बढ़ कर शत्रुता में बदल जाए, तो वह उसे मिटाने पर तुल जाता है और अगर शत्रुता की भावना और अधिक प्रबल हो जाए, तो वह उसके विनाश को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है और हाथ धोकर उसके पीछे इस प्रकार पड़ जाता है कि जब तक वह उसे मिटा नहीं देता,चैन नहीं लेता। इसी तरह जब उसे कोई चीज़ पसंद आती है तो वह उसे अपना लेता है। जब प्यार करता है, तो अपनी आँखों से उसे देखकर और अपने कानों से उसका ज़िक्र सुनकर ख़ुशी होती है। जब प्रेम से बढ़कर इश्क़ का दर्जा हासिल हो जाता है, तो चाहता है कि दुनिया के कण-कण में उसी की सुंदरता हो और जीवन का एक भी क्षण उसके सिवा किसी अन्य को देखने, अन्य का उल्लेख सुनने और अन्य की कल्पना करने में व्यर्थ न जाए। फिर अगर यह इश्क़ और बढ़ जाए तो वह अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर देता है और अपना जीवन और धन, वैभव, मान-प्रतिष्ठा सब कुछ उस पर न्योछावर कर देता है। “अम्र बिल-मारूफ़” जिस चीज़ का नाम है, वह भलाई से इश्क़ की प्राकाष्ठा है और “नह्यि अनिल-मुनकर” द्वारा जिस भाव को व्यक्त किया गया है, वह वास्तव में बुराई से घृणा और शत्रुता की सर्वोच्च सीमा है। “मारूफ़” का आदेश देने वाला मात्र नेक ही नहीं होता, बल्कि वह अच्छाई का आशिक़ और उसपर सर्वस्य लुटाने वाला होता है, और जो “मुन्कर” को रोकता है, वह न केवल बुराई से बचा रहता है, बल्कि वह उसका शत्रु है, और उसके ख़ून का प्यासा है।
एक और तत्व जिस पर “अम्र बिल-मारूफ़” और “नह्यि अनिल-मुनकर” की नींव स्थापित होती है, वह मानवता के प्रति सहानुभूति और करुणा है। एक स्वार्थी व्यक्ति उस कृपा में अकेला रहना चाहता है जो अल्लाह उसे देता है, और इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करता है। इसी प्रकार अगर उस पर कोई संकट आ पड़े तो वह उससे बचने का भरसक प्रयत्न करता है, पर दूसरों को संकट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति करुणामय और मानवता से प्रेम करने वाला है, वह सबके साथ अपनी सुख-सुविधा बांटता है, सबके साथ अपना प्रेम बांटता है और जब वह दूसरों को संकट में देखता है, तो वह उसी प्रकार व्याकुल हो उठता है, जैसे अपने लिए हो सकता है।
मानवता का सच्चा हितैषी स्वयं सदाचारी बनकर संतुष्ट नहीं हो सकता। तब तक वह मानव समुदाय के अन्य सदस्यों को बुराई के चंगुल से मुक्त नहीं कर देता और उन्हें अच्छाई का मार्ग नहीं दिखा देता, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अपने दूसरे भाई को बुराई से पीड़ित देखकर उसकी आत्मा बेचैन रहती है। जब वह किसी चीज़ की अच्छाई जान लेता है तो चाहता है कि सभी लोगों को उसका लाभ मिले, और जब वह किसी चीज़ की बुराई जान लेता है तो वह चाहता है कि एक भी व्यक्ति उसके चंगुल में फंसा न रहे। अपनी भलाई से संतुष्ट होकर दूसरों का भला न चाहना और स्वयं से बुराई को दूर करके संतुष्ट रहना और दूसरों को उससे बचाने की कोशिश न करना, सबसे बड़ा स्वार्थ है।
यह केवल स्वार्थ ही नहीं आत्मघात भी है। मनुष्य एक सभ्य प्राणी है, वह समुदाय से अलग होकर जीवन नहीं बिता सकता। उसकी भलाई और बुराई सब कुछ सामूहिक है। समूह बुरा होगा, तो उसकी बुराई से वह भी बच नहीं पाएगा। अगर कोई शहर प्रदूषित हो और उसमें महामारी फैल जाए, तो यह प्रदूषण केवल उसी व्यक्ति के लिए घातक नहीं होगा, जिसका घर प्रदूषित हो, बल्कि उस स्वच्छ व्यक्ति को भी संक्रमित करेगा जो प्रतिदिन स्नान करता है और अपने घर को साफ़ करता है। इसी प्रकार अगर किसी बस्ती का सामान्य आचार बिगड़ा हुआ हो और वहाँ के लोग सामान्यतया बुरे हों, तो उस पर जो विनाश उतरेगा वह केवल दुष्टों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु उन थोड़े से नेक काम करने वालों की इज़्ज़त और प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो उस बस्ती में रहते हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस विषय को एक हदीस में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है:
अल्लाह आम लोगों पर ख़ास लोगों के कामों के चलते तब तक विनाश नहीं उतारता जब तक कि उनमें यह दोष पैदा न हो जाए कि अपने सामने बुरे कर्मों को होता हुआ देखें और उन्हें रोकने की ताक़त रखते हों, मगर उन्हें न रोकें। जब वे ऐसा करने लगते हैं तो अल्लाह आम और ख़ास सब पर अज़ाब नाज़िल करता है।” (मुस्नद अहमद)
अतः “अम्र बिल-मारूफ़” और “नह्यि अनिल-मुनकर” केवल दूसरों की सेवा ही नहीं है, बल्कि स्वयं की सेवा भी है, और वास्तव में, समग्र सुधार में स्वयं के सुधार की इच्छा की बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है।
सामूहिक जीवन में भलाई के आदेश और बुराई के निषेध की अवधारणा की स्थिति
तो यही वह चीज़ है जिस पर सामूहिक कल्याण निर्भर करता है, जो एक राष्ट्र और एक समाज को नष्ट होने से बचाता है, जिसके बिना मानवता की रक्षा नहीं की जा सकती। जब तक कि एक राष्ट्र में यह भावना मौजूद रहती है, कि उसके लोग एक दूसरे को अच्छाई का आदेश दें और बुराई से रोकें, या कम से कम उस राष्ट्र में एक समूह ऐसा मौजूद है जो इस दायित्व को पूरी लगन से निभाता रहे, तो वह राष्ट्र कभी नष्ट नहीं हो सकता। परन्तु अगर उसमें से “अम्र बिल-मारूफ़” और “नह्यि अनिल-मुनकर” की यह आत्मा निकल जाए, और उस में ऐसा कोई समूह भी न रह जाए, जो इस दायित्व को पूरा करने वाला हो, तो धीरे धीरे उस पर बुराई का शैतान आच्छादित हो जाता है, और अन्त में वह विनाश के गड्ढे में ऐसा गिरता है कि कभी उभर नहीं सकता। इसी तथ्य का वर्णन पवित्र क़ुरआन में इस प्रकार किया गया है:
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُو۟لُوا۟ بَقِيَّةٍۢ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ○ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○ (ہود: ۱۱۶۔۱۱۷)
“तो तुमसे पहले की क़ौमों में (जिन्हें दण्ड दिया गया) ऐसे सदाचारी क्यों नहीं हुए, जो उन्हें धरती में उपद्रव करने से रोकते? ऐसे लोग बहुत थोड़े थे, जिन्हें हमने उनमें से बचा लिया वरना सभी ज़ालिम लोग अपनी मौज-मस्ती में लगे रहे ,जिनके संसाधन उन्हें दिये गये थे और वे अपराधी बन कर रहे। और तुम्हारा पालनहार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अत्याचार से ध्वस्त कर दे, जबकि उनके वासी भले लोग हों” (हूद :116-117)
एक अन्य स्थान पर बनी इसराईल के अभिशाप का कारण यह बताया गया है कि:
لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ○ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ○ (المائدہ: ۷۸-۷۹)
“इसराईल की संतानों में से अल्लाह की अवज्ञा करने वाले लोगों पर दाऊद और मरयम के बेटे ईसा द्वारा अभिशाप भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की और अपराध किया, वे एक दूसरे को उन बुरे कामों से नहीं रोकते थे, जो वे किया करते थे और यह बहुत बुरा था जो वे करने में अभयस्त थे।” (अल-माइदा : 78-79)
इस आयत की व्याख्या में, इमाम अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, और इब्न माजा द्वारा सुनाई गई हदीसों में थोड़े अंतर के साथ कहा गया है कि बनी इसराईल (इसराईल की संतान) के बीच पैदा होने वाला पहला दोष यह था कि उनके दिलों से बुराई के लिए नफरत दूर हो गई और वह झूठी सहनशीलता पैदा हो गई थी जो बुराई को सहन करते हुए आदमी को ख़ुद भी बुराई में लिप्त हो जाने के लिए तैयार कर लेती है। जब उनमें का एक आदमी दूसरे से मिलता तो वह कहता है, “ऐ आदमी, अल्लाह से डरो, और यह काम छोड़ दो, जो तुम करते हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए जायज़ नही, लेकिन जब आप उससे अगले दिन मिलता, तो कोई भी चीज़ उसको उसी बुराई में लिप्त होने से न रोकती। आख़िर, वे एक-दूसरे की बुराई से प्रभावित हो गए और उनका विवेक मर गया।
जब पैग़म्बर (सल्ल.) हमसे यह कह रहे थे, तो आप एक़दम चौकन्ना हो उठे और जोश में आकर कहा:
“उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम पर अनिवार्य है कि भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, और बुराई करने वाले का हाथ पकड़ लो और उसे सत्य की ओर मोड़ दो, नहीं तो अल्लाह तुम्हारे दिलों पर भी उसका असर डाल देगा और तुम पर भी उसी तरह लानत (अभिशाप) करेगा जिस तरह उन लोगों पर की थी।”
जिस प्रकार किसी राष्ट्र का कल्याण और उसकी मुक्ति “मारूफ़” (भलाई) का आदेश देने और “मुन्कर” (बुराई) से रोकने की व्यावहारिक भावना पर निर्भर करता है, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जगत का उद्धार और कल्याण भी उसी पर निर्भर करता है। दुनिया में कम से कम एक समुदाय ऐसा अवश्य होना चाहिए जो ज़ालिमों का हाथ पकड़े और बुराई से रोके, और अच्छे कामों का आदेश देता हो, अल्लाह की ओर से धरती पर गवाह हो, लोगों की देख-भाल करता रहे, असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में रखे, न्याय स्थापित करे और बुराई को कभी सर उठाने का अवसर न दे। अल्लाह की रचना को सामान्य विनाश से बचाने के लिए और उसकी भूमि को बुराई और बिगाड़ और अत्याचार से बचाने के लिए ऐसे समुदाय का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है।
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ○ (آل عمران : ۱۰۴)
“और तुम में एक समुदाय ऐसा अवश्य होना चाहिए जो भलाई की ओर बुलाए, नेकी का आदेश दे, और बुराई से रोके।” (आले-इमरान: 104)
इसलिए, ''अम्र बिल-मारूफ़ और नह्यी अनिल-मुनकर'' की सच्चाई केवल यह नहीं है कि वह अपने आप में एक अच्छी चीज़ है और करुणा मानव जाति की एक शुद्ध भावना है, बल्कि वास्तव में यह सभ्य व्यवस्था को बिगाड़ से बचाने के लिए एक उत्कृष्ट और अनिवार्य रणनीति है। यह एक सेवा है जिसे अल्लाह ने दुनिया में शांति स्थापित करने और दुनिया के लोगों को पशुता से ऊपर उठाकर पूर्ण मानवता के स्तर तक लाने और दुनिया को सभ्य और सुशील लोगों के रहने योग्य बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सौंपा है।
भलाई के आदेश और बुराई के निषेध का अंतर
यह सार्वभौमिक मानव सेवा जो अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय को सौंपी गई है, उसमें दो घटक शामिल हैं, एक ''अम्र बिल-मारूफ़” और दूसरे “नह्यी अनिल-मुनकर'' अर्थात अच्छाई का आदेश देना, और दूसरा बुराई से रोकना। यद्यपि दोनों का लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है, अर्थात् आदमी को इनसान बनाना, परन्तु दोनों के दर्जे भिन्न-भिन्न हैं, अतः दोनों के तरीक़ों में भी अन्तर है। इस अंतर को समझ लेना महत्वपूर्ण है।
नैतिकशास्त्र में मानव दायित्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक वैसे दायित्व जिनके करने की उस से मांग की जा सकती है। दूसरे वैसे दायित्व जिनका करना या नहीं करना उसकी अपनी मर्ज़ी पर है। समाज का अच्छा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम दायित्व यह है कि वह बुरे कामों से बचे, दूसरों के अधिकारों को न छीने, दूसरों के साथ अन्याय न करे, दूसरों की शांति और सुरक्षा को भंग न करे और ऐसे कार्यों से परहेज़ करे, जो इसके अस्तित्व को समाज के लिए हानिकारक या अनुपयोगी बना दे। प्रत्येक समाज को अपने समाज के प्रत्येक सदस्य से इन दायित्वों का पालन करने की ज़रूरत होती है, और अगर वह उन्हें नहीं करता है, तो उसे उन्हें करने के लिए बाध्य करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे प्रकार का दायित्व नैतिक गुणों से संबंधित है, जिसके पालन से व्यक्ति समाज का एक सम्मानित और उच्च श्रेणी का कार्यकर्ता बन सकता है। उदाहरण के लिए, अल्लाह और बन्दों के अधिकारों को पहचानना और उन्हें पूरा करना, स्वयं अच्छे बनना और दूसरों को अच्छा बनाना, अपने परिवार और अपने राष्ट्र और समस्त मानव जाति की सेवा करना और सत्य का समर्थन और रक्षा करना, आदि। इस दूसरे प्रकार के दायित्व को निभाने के लिए मानवीय चेतना का निर्मान आवश्यक है। कोई उन्हें तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि वह उनकी वास्तविकता को अच्छी तरह से न समझ ले और स्वयं में इतना शुद्ध न हो जाए कि वह उन्हें पूरा करने को ख़ुद से तैयार हो। इसलिए, ये दायित्व अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक हैं और व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, कि वह सम्मानजनक और उच्च दर्जे का इनसान बने या न बने। यद्यपि समाज की नैतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसके सदस्यों में स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर पहुँचने की इच्छा पैदा हो।
''अम्र बिल-मारूफ़” और “नह्यी अनिल-मुनकर'' के बीच का अंतर भी लगभग उसी विभाजन पर आधारित है। मनुष्य को पशुता के गड्ढे से बाहर निकालकर उसे मानवता के स्तर पर लाना और उसे मानव समाज का अनुपयोगी और हानिकारक सदस्य बनने से रोकना, “नह्यी अनिल-मुनकर'' के अंतर्गत आता है। फिर उसे मानवता के स्तर से ऊपर उठाकर पूर्ण मानवता के स्तर तक लाना और उसे मानव समाज का एक उपयोगी और सम्मानित सदस्य बनाना ''अम्र बिल-मारूफ़” से संबंधित है। ''अम्र बिल-मारूफ़”, “नह्यी अनिल-मुनकर'' अर्थात भलाई का आदेश देना बुराई से रोकने से उत्तम है। परन्तु क्रम के आधार पर “नह्यी अनिल-मुनकर'' पहले है और ''अम्र बिल-मारूफ़” बाद में है। जिस तरह एक किसान का मुख्य लक्ष्य अनाज पैदा करना होता है, लेकिन इसके लिए बीज बोने से पहले जुताई करके मिट्टी को नरम करना आवश्यक है। इसी तरह इस्लाम का मुख्य उद्देश्य तो इंसान को श्रेष्ठ इंसान बनाना है, लेकिन अच्छाई का बीज बोने से पहले उसकी प्रकृति को मुनकर से मुक्त करना और उसे समतल बनाना आवश्यक है। इस्लाम सभी को नेकियों की ओर बुलाता है और इसके गुण दिखाकर लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन मुनकर एक ऐसा परदा है जो मनुष्य की आंख को मारूफ़ को स्वीकार करने में समर्थ नहीं होने देता। इसलिए सर्वप्रथम और सबसे आवश्यक उपाय यह है कि मुनकर के परदे को हर संभव तरीक़े से चीर दिया जाए और उसके जंग को हर संभव तरीक़े से खुरच दिया जाए। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मारूफ़ के निमंत्रण को स्वीकार करता है, तो उसके लिए नैतिक गुणों का एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पूर्ण मानवता की श्रेणी तक पहुँचने के बाद, उसके लिए वे सहजताएं बाक़ी नहीं रह सकतीं, जो मानवता के पहले चरण में उसे प्राप्त थीं।
एक दूसरी हदीस में ''अम्र बिल-मारूफ़” और “नह्यी अनिल-मुनकर'' का अंतर उस अंतर पर निर्भर है, जो ख़ुद इस्लाम के दो अलग-अलग स्वरूपों के बीच है। एक स्थिति में इस्लाम केवल अच्छाई और परहेज़गारी का आह्वान है और दूसरी स्थिति में यह अल्लाह का क़ानून है, जो पूरी दुनिया के लिए है। जब कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए ये दोनों स्वरूप जमा हो जाते हैं और उसके पक्ष में दावत (आह्वान) के प्रावधान भी बदल जाते हैं। दावत का उद्देश्य यह है कि मनुष्य उस ख़िलाफ़त के योग्य हो जाए है जो अल्लाह ने उसे धरती पर भेजते समय सौंपी थी और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करे जो उस पर ज़मीन पर अल्लाह के ख़लीफ़ा होने के रूप में आती हैं। क़ानून का उद्देश्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति ख़िलाफ़त की सेवाओं को पूरा नहीं करता है, तो कम से कम वह ज़मीन में बिगाड़ और रक्तपात तो न करे, जिसका उलाहना फ़रिश्तों ने उसे दिया था। अगर वह अशरफ़ुल-मख़लुक़ात (सर्वश्रेष्ठ रचना) नहीं बनता है तो कम से कम अर्जल-उल-मख़लूक़ात (निकृष्ट रचना) तो न बने। पहला चीज़ आंतरिक प्रकाश और प्रवृति की क्षमता पर निर्भर है, जो स्पष्ट है कि बलपूर्वक पैदा नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी चीज़ सीमाओं के निर्धारण और रखरखाव से जुड़ी है, जिसके लिए उसकी विद्रोही प्रवृति को केवल उपदेशों द्वारा ही प्रेरित नहीं किया जा सकता है, बल्कि कुछ स्थितियों में उसे मजबूर करने के लिए बल का प्रयोग भी आवश्यक होता है।
बुराई से रोकने की कार्यप्रणाली
इस लेख के कुछ पहलुओं पर और प्रकाश डालने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम किसी अन्य अवसर पर विस्तार से बताएंगे। यहाँ केवल यह कहने का आशय है कि इस्लाम ने ग़ैर-मुस्लिम दुनिया को भलाई की प्रेरणा देने के लिए तो केवल निमंत्रण देने और उपदेश देने का तरीक़ा बताया है, लेकिन बुराई से रोकने के लिए इसकी सीमा नहीं रखी, बल्कि इसके विभिन्न प्रकारों के लिए अलग-अलग तरीक़े सुझाए गए हैं। हृदय और मन की अशुद्धता और सोच-विचारों की गंदगी को उपदेशों के माध्यम से दूर करने का निर्देश दिया:
ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ○ (النحل :۱۲۵)
“आप उन्हें अपने पालनहार की राह (इस्लाम) की ओर तत्वदर्शिता तथा सदुपदेश के साथ बुलाएँ और उनसे ऐसे अंदाज़ में बातचीत करें, जो उत्तम (अर्थात् वह कठोर न हो और उसनें अपशब्द न हो)।” (अल-नह्ल: 125)।
۞ وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ۔۔۔ (العنکبوت :۴۶)
“और अहले किताब (यहूदी और ईसाई) के साथ बेहतरीन तरीक़े से बहस करो, सिवाए उनके जो उन में दुष्ट और अत्याचारी हैं।” (अल-अनकबूत: 46)
فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًۭا لَّيِّنًۭا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ○ (طٰہٰ :۴۴)
उस विद्रोही व्यक्ति से नर्मी से बात करो, शायद कि वह सुधर जाए और अल्लाह से डरे।” (ता-हा:44)
बुराई को बलप्रयोग के माध्यम से रोकने का आदेश दिया। ऊपर वह हदीस आ चुकी है जिसमें पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा: “यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम दुष्ट का हाथ पकड़ लो और उसे सत्य की ओर मोड़ दो। इसके अलावा, कई हदीसें ऐसी हैं जिनमें मुनकर को रोकने के लिए बल प्रयोग का आदेश दिया गया है। एक जगह अल्लाह के रसूल (सल्ल.) कहते हैं:
तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उस को हाथ से बदल दे, अगर उसकी क्षमता न रखता हो, तो कथन से और अगर उसकी क्षमता भी न रखता हो तो दिल से, और यह ईमान का सबसे कमज़ोर स्तर है। (मुस्लिम)
“इन हदीसों में, “हाथ” शब्द का प्रयोग मात्र शारीरिक हाथ के अर्थ में नहीं, बल्कि शक्ति और बल के अर्थ में किया गया है। एक बुराई करने वाले का हाथ पकड़ने का अर्थ वास्तव में ऐसी स्थिति पैदा करना है कि वह बुराई न कर सके। इसी तरह, हाथ से बुराई को बदलने का मतलब है कि अपनी ताक़त और शक्ति का उपयोग बुराई को मिटाने और उसे अच्छाई से बदल देने में किया जाए। एक और हदीस कहती है:
“अल्लाह आम लोगों को ख़ास लोगों के कामों की सज़ा तब तक नहीं देता जब तक कि उनमें यह झूठी सहनशीलता विकसित न हो जाए, कि बुराई को अपने सामने होते हुए देखें और उसे रोकने की ताक़त रखते हों, मगर न रोकें।” (मुस्नद अहमद)
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) का बयान अल्लाह के बयान की व्याख्या होता है। इसलिए, इन हदीसों से पवित्र क़ुरआन के आदेश 'नह्यी अनिल-मुनकर' का अर्थ स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाता है। इसका अर्थ केवल बोलकर या लिखकर ही बुराई को रोकना और उसके ख़िलाफ़ उपदेश देना नहीं है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसे बलपूर्वक रोकना और संसार को उसके अस्तित्व से मुक्त कर देना भी है। यह मुसलमानों की शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर मुसलमानों के पास पर्याप्त शक्ति है कि वे पूरी दुनिया को ‘मुनकर’ से रोक कर न्याय के क़ानून के प्रति आज्ञाकारी बना दें, तो उनका दायित्व है कि वे इस शक्ति का उपयोग करें और तब तक चैन न लें जब तक कि वे इस कार्य को पूरा न कर लें, लेकिन अगर वे ऐसा करते में सामर्थ्य नहीं है, तो जहाँ तक हो उन्हें इस काम को करना चाहिए और इस काम को पूरा करने के लिए और अधिक बल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
फ़ितना (षडयंत्र) और फ़साद (बिगाड़) के ख़िलाफ़ युद्ध
बुराई की इस दूसरी क़िस्म को जिसके ख़िलाफ़ इस्लाम में बलप्रयोग का आदेश दिया गया है पहली क़िस्म से उसकी प्रकृति को और स्पष्ट करने के लिए अल्लाह ने इसे ‘फ़ित्ना’ और ‘फ़साद’ के शब्दों से परिभाषित किया है। इसलिए उन सभी आयतों में, जिनमें ‘मुनकर’ (बुराई) के विरुद्ध युद्ध की अनुमति दी गई है, या युद्ध की ज़रूरत दिखाई गई है, या तलवार से मिटाने का आदेश दिया गया है, उसमें मुनकर के स्थान पर फ़ितना (षडयंत्र) और फ़साद (बिगाड़) के शब्द मिलेंगे।
وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ۔۔۔ (البقرہ ۱۹۳ اور الانفال ۳۹)
और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ित्ना बाक़ी न रहे, (अल-बक़रह : 193, अल-अनफ़ाल: 39)
وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ۔۔۔ (البقرہ: ۲۵۱)
“अगर अल्लाह उन लोगों को एक दूसरे के माध्यम से ठिकाने न लगाता तो धरती फ़साद से भर जाती।” (अल-बकरा: 251)
بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌۭ كَبِيرٌۭ○ (الانفال: ۷۳)
“अगर तुम ऐसा न करोगे, तो धरती पर फ़ितना और भारी फ़साद होगा।” (अल-अनफ़ाल: 73)।
أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ (البقرہ: ۱۹۱)
“और फ़ित्ना क़त्ल से भी बुरा है।” (अल-बक़रह: 191)
مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا۔۔۔ (المائدہ : ۳۲)
जो कोई किसी की हत्या करता है, बिना इसके कि उस ने किसी की जान ली हो या ज़मीन में फ़साद फैलाया हो तो मानो उसने सभी लोगों की हत्या कर दी।” (अल माइदाः 32)
لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ۔ (التوبہ :۴۸)
“वे फ़ितना फैलाना चाहते थे।” (अत्तौबा : 48)
كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ (النساء :۹۱)
“जब कभी आप फ़ितना की ओर वापस जाते हैं, तो आप स्वयं उसमें शामिल हो जाते हैं।” (अल-निसा: 91)
इन सभी आयतों में उसी मुनकर को फ़ितना और फ़साद के शब्दों से परिभाषित किया गया है। तथ्य यह है कि सभी बुराइयों में, यह फ़ित्ना और फ़साद ही एक ऐसी चीज़ है जिसे तलवार के बिना नहीं मिटाया जा सकता है।
फ़ितना (षडयंत्र) की जांच
आम तौर पर फ़ित्ना और फ़साद का अर्थ यह समझा जाता है कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, पहले झगड़ा हो, फिर दोनों पक्ष के बलवान लोग ईंट, पत्थर, लाठी या तलवार और बन्दूक़ लेकर मैदान में कूद पड़ें। एक दूसरे के सिर, फोड़ें और अच्छी तरह से हत्याएं करके उग्र क्रोध को शांत करें। वैसे तो इस को भी फ़ितना और फ़साद कहते हैं, लेकिन क़ुरआन की शब्दावली में इन शब्दों का मतलब इतना संकीर्ण नहीं है, बल्कि और बहुत से नैतिक अपराध भी इनके अंतर्गत आते हैं। हमें अन्य किताबों में उनके विवरणों की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क़ुरआन स्वयं हमें बताता है कि फ़ित्ना और फ़साद से उसका आशय क्या है।
पवित्र क़ुरआन के अनुसार फ़ित्ना का सही अर्थ परीक्षा और परीक्षण है, चाहे वह लाभ के लालच के माध्यम से हो, या हानि के भय और पीड़ा के माध्यम से हो। अगर यह परीक्षा अल्लाह की ओर से है तो ठीक है क्योंकि अल्लाह मनुष्य का रचयिता है और उसे अपने बन्दों की परीक्षा लेने का अधिकार है और उसकी परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर और उच्च अवस्था की ओर ले जाना है। लेकिन अगर यह परीक्षण एक मनुष्य द्वारा किया जाता है तो यह क्रूरता है क्योंकि एक मनुष्य को इसका अधिकार नहीं है, और जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को फ़ितने में डालता है, तो उसका उद्देश्य उसकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता को नष्ट करना, उसे अपनी दासता के लिए बाध्य करना और उसे नैतिक और आध्यात्मिक पतन में ले जाना होता है। क़ुरआन में दिए गए इसके विवरण इस प्रकार हैं:
(1) कमज़ोरों पर अत्याचार करना, उनके वैध अधिकारों का हनन करना, उनके घरों को लूटना और उन्हें कष्ट देना:
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ثُمَّ جَـٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓ۔۔۔(النحل: ۱۱۰)
“फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए (क्षमादान करने वाला है) जो फ़ितने में डाले जाने (प्रताड़ित किए जाने) के बाद अपने घरों को छोड़ कर निकल गए, और उन्होंने हक़ के लिए बहुत जिद्दो-जेहद की और हक़ की राह पर अडिग रहे।” (अल-नहल: 110)
ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ (البقرہ : ۲۱۷)
“(पवित्र महीनों के दौरान लड़ना निश्चित रूप से पवित्र मस्जिद (काबा) के अधिकार का उल्लंघन है) लेकिन काबा के निवासियों को वहां से निकालना अल्लाह की दृष्टि में इससे भी बुरा है, और फ़ितना हत्या से भी बदतर है।” (अल-बक़रह: 217)
2. दमन और अत्याचार के साथ सच को दबाना और लोगों को सच मानने से रोकना:
فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍۢ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ (یونس: ۸۳)
“सो जवानों के एक छोटे दल को छोड़ उनके लोगों में से किसी ने मूसा पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे फ़िरऔन और उनके सरदारों से (जो फ़िरऔन के चाटुकार थे) डरते थे, कि कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें फ़ितने में डाल दें।” (यूनुस : 83)
(3) अल्लाह के मार्ग से रोकना: जिसकी व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है।
(4) लोगों को गुमराह करना और सत्य के ख़िलाफ़ कपट, लालच और बल का प्रयोग करना:
وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًۭا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًۭا○ (بنی اسرائیل : ۷۳)
“और वे चाहते थे कि तुम्हें लालच और घृणा के द्वारा उस प्रकाशना से दूर कर दें जो हमने तुम पर भेजी है, ताकि तुम उसे छोड़ दो और हम पर आरोप लगाओ (अगर तुमने ऐसा किया होता), तो वे तुम्हें मित्र बना लेते।” (बनी इसराईल: 73)
أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ (المائدۃ ۴۹-۵۰)
“और उनसे सचेत रहो कि कहीं वे तुम्हें धोखा देकर उनमें से कुछ चीज़ों से विचलित न कर दें जो अल्लाह ने तुम पर उतारी हैं। क्या वे इस्लामपूर्व अरब का फ़ैसला चाहते हैं?” (अल-मायदाः 49-50)
5. असत्य के लिए युद्ध छेड़ना और एक अन्यायपूर्ण कारण के लिए मारना और मरना:
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَـَٔاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًۭا ○ (الاحزاب : ۱۴)
“(अहज़ाब के युद्ध के अवसर पर) अगर दुश्मन मदीना की ओर से प्रवेश करते हैं और फिर उन्हें (मुनाफिकों) को फ़ित्ना में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है, तो वे ज़रूर उसमें कूद पड़ते और तनिक संकोच नहीं करते।” (अल-अहज़ाब: 14)
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ (النساء : ۹۱)
“तुम्हें (इन कपटाचारियों में से) कुछ दूसरे लोग ऐसे पाओगे जो तुम से भी शांति में रहना चाहते हैं और अपनी क़ौम से भी, लेकिन जब वे फ़ितना की ओर फेर दिए जाते हैं, तो वे उसमें औंधे गिर जाते हैं।” (ख़ुदभी फ़ितना खड़ा करने वालों में शरीक हो जाते हैं) (अन्निसा :91)
6 सत्य के अनुयायियों पर असत्य के उपासकों का प्रभुत्व:
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌۭ كَبِيرٌۭ○ (الانفال : ۷۳)
“अगर तुम (सत्य के अनुयायियों की सहायता) नहीं करोगे, तो ज़मीन में एक फ़ितना और बड़ा फ़साद आएगा, अर्थात् असत्य के प्रभुत्व से सत्य के अनुयायियों पर ज़मीन संकुचित हो जाएगी।” (अल-अनफ़ाल: 73)
फ़साद (बिगाड़) की जांच
अब देखिए पवित्र क़ुरआन में बिगाड़ शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया गया है।
शब्दकोश में, फ़साद कहते हैं किसी चीज़ के संतुलन की अवस्था से निकल जाने को यह सुधार और बनाव का विलोम है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्रत्येक कार्य जो न्याय और संतुलन के विरुद्ध हो वह ‘फ़साद’ है। लेकिन पवित्र क़ुरआन में, इसे आम तौर पर सामूहिक नैतिकता, सभ्यता और राजनैतिक व्यवस्था के बिगाड़ के अर्थ इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए, क़ुरआन फ़िरऔन, आद और समूद पर बिगाड़ का आरोप लगाता है:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ○ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ○ ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَـٰدِ ○ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ○ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ ○ ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ ○ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ○ ( الفجر : ۶-۱۲)
“क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पालनहार ने “आद” के साथ क्या किया? स्तम्भों वाले “इरम” के साथ? जिनके समान देशों में लोग नहीं पैदा किये गये। तथा “समूद” के साथ जिन्होंने घाटियों मे चट्टानों को काट रखा था। और कीलों वाले फ़िरऔन के साथ। जिन्होंने नगरों में फ़साद (उपद्रव) मचा रखा था।” (अल-फ़ज्र : 6-12)
फिर, विभिन्न स्थानों पर, क़ुरआन उनके उन अपराधों का वर्णन करता है, जिनके आधार पर उन्हें फ़सादी ठहराया गया:
1. फ़िरऔन के बारे में कहा, कि वह अहंकारी था, अपनी प्रजा के बीच जातीय भेद स्थापित करता था और उन्हें विभाजित करके उन पर शासन करता था, और कमज़ोरों को अन्यायपूर्वक मारता और लूटता था:
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ○ (قصص:۴)
“फ़िरऔन उस देश में अहंकार करने लगा, और उसके रहने वालों के दल बांटकर एक दल को क्षीण किया, और उनके बेटों को घात करने और उनकी स्त्रियों को जीवित रखने लगा। वास्तव में वह फ़सादी लोगों में से था।।” (अल-क़सस : 4)
वह लोगों को जबरन सत्य स्वीकार करने से रोकता था और लोगों पर अत्याचार करता था। इसलिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार देखकर जादूगर ईमान ले आए, तो उसने कहा:
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ○ (طٰہٰ :۷۱)
“मेरे द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले तुम ईमान ले आए? निश्चय ही यही तुम्हारा गुरु हैं और उन्होंने ही तुम्हें यह जादू सिखाया है। अब मैं तुम्हारे हाथ-पांव विपरीत दिशा से काट डालूंगा और तुम्हें खजूर के तने पर सूली चढ़ा दूंगा और तुम देख लोगे कि हममें से सबसे कठोर और देर तक चलने वाला दण्ड कौन है।”
उसने एक क़ौम को कमज़ोर पाया और उसे अपना ग़ुलाम बना लिया था। इसलिए, जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एहसान जताया, तो उन्होंने उत्तर दिया:
وَتِلْكَ نِعْمَةٌۭ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيل○(الشعرا:۲۲)
“और तेरी वह नेमत जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है, वह यह है कि तूने मेरी क़ौम बनी इसराईल को ग़ुलाम बना लिया है।” (अश्शुअरा: 22)
अपनी शक्ति के नशे में चूर, वह अपने जैसे लोगों का देवता बनता था और केवल बल के आधार पर शासन करता था, हालाँकि वास्तविक अधिकार तो न्याय और अल्लाह की बन्दगी का है।
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًۭا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ . وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ○ (القصص : ۳۸ -۳۹)
“और फ़िरऔन ने कहाः लोगो! मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी पूज्य को नहीं जानता।... और उसने तथा उसकी सेनाओं ने धरती में अवैध रूप से घमंड किया और उन्होंने समझा कि वे हमारी ओर वापस नहीं लाये जाएंगे। (अल-क़सस: 38-39)
उसने अपनी प्रजा की मानसिक और नैतिक स्थिति को इतना नीचे गिरा दिया था कि वे उसकी ग़ुलामी के लिए राज़ी हो गए:
فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ○ (الزخرف: ۵۴)
“उसने अपनी क़ौम को हल्का (यानि बुद्धि और नैतिकता में हीन) बना दिया जिसके कारण उन्होंने उसकी आज्ञाकारिता स्वीकार की, निश्चय ही वे दुष्कर्मी लोग थे।” (अल-ज़ुख़रुफ़: 54)
उसके शासन की बुनियाद अवैध और ग़लत क़ानून पर रखी गई थी:
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍۢ○ (ھود : ۹۷)
“उन लोगों ने फ़िरऔन की आज्ञाओं का पालन किया, यद्यपि फ़िरऔन का आदेश सत्य पर आधारित नहीं था।” (हूद: 97)
2. इसी प्रकार आद का अपराध यह बताया गया है कि वे दमन करने वाले अत्याचारी शासकों का अनुसरण करते थे:
وَتِلْكَ عَادٌۭ ۖ جَحَدُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا۟ رُسُلَهُۥ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍۢ○ (ھود: ۵۹)
“उन्होंने हर अत्याचारी, सत्य के दुश्मन के आदेश का पालन किया।” (हूद: 59)
वे अत्याचारी और क्रूर थे और न्याय और निष्पक्षता की कोई परवाह नहीं करते थे, इसलिए हज़रत हूद ने उन्हें धिक्कारा और कहा:
وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ○ (الشعراء :۱۳۰)
“और तुम जिस पर जिस पर भी हाथ डालते हो क्रूरता के साथ ही डालते हो।” (अश्शुअरा:130)
और वे अपने बल के घमण्ड में निर्बल जातियों पर बिना अधिकार के राज्य करते थे:
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ○ (حٰم السجدہ : ۱۵)
“सो वे बिना सत्य के धरती में अहंकार करने लगे और कहने लगे, “हम से अधिक शक्तिशाली कौन है?” (हा-मीम अस्सजदा: 15)
(2) समूद के विध्वंसक कार्यों की व्याख्या पवित्र क़ुरआन में यह मिलती है कि उनके शासक और प्रमुख क्रूर और दुष्ट थे और वे उन्हीं प्रमुखों का अनुपालन करते थे, इसलिए हज़रत सालेह उन्हें उपदेश देते हैं:
وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ○ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ○(الشعراء : ۱۵۱-۱۵۲)
“और उन ज़ालिमों के आदेशों का पालन न करो जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं और उसमें सुधार नहीं करते।” (अश्शुअरा: 151-152)
वे इतने उद्दंड थे कि वे एक सच बोलने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए मारने को तैयार हो गए कि वह उन्हें बुराई करने से रोकता था और उन्हें भलाई करने के लिए प्रेरित करता था, और फिर इस क्रूर कार्य को करने के लिए छल-कपट की बुरी चालों का सहारा लेने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ:
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨ قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ○ (النمل: ۴۸-۴۹)
“और उस नगर में नौ व्यक्ति (समूहों के प्रमुख) थे, जो देश में उत्पात मचाते थे और सुधार नहीं करते थे। उन्होंने कहा, “मेरे दोस्तो! क़सम खाओ कि रात सालेह और उसके परिवार पर छापा मारेंगे और उसके ख़ून के दावेदारों से कह देंगे कि हमें उसकी और उसके परिवार की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता है और हम सच बोलते हैं।” (अन्नमल :48-49)
4. पवित्र क़ुरआन में, लूत के लोगों को भी फ़सादी कहा गया है और उनके बिगाड़ को इस प्रकार व्यक्त किया गया है:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ ○ (عنکبوت: ۲۸-۲۹)
“और लूत को (भेजा)। जब उसने अपनी क़ौम से कहाः तुम तो वह दुष्कर्म और निर्लज्जता के काम कर रहे हो, जो तुमसे पहले संसार वासियों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम पुरुषों के पास अपनी वासना पूरी करने जाते हो और लूट-पाट करते हो तथा अपनी सभाओं में खुल्लम-खुल्ला निर्लज्जा के कार्य करते हो?” (अनकबूत:28-29)
यह उस क़ौम का बिगाड़ था कि प्रकृति के विपरीत कार्य करना आम बात हो गई थी, वह व्यापारिक राजमार्गों पर लूट-पाट भी करती थी और उसकी सामूहिक नैतिकता इस हद तक बिगड़ गई थी कि वे अपनी सभाओं में खुलेआम दुष्कर्म करते थे और कोई उन्हें टोकने वाला नहीं था।
(5.) मदयन के लोगों को भी फ़सादी कहा गया है और हज़रत शुऐब उन्हें इन शब्दों में उपदेश देते हैं:
فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍۢ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًۭا ۚ○ (اعراف: ۸۵-۸۶)
“नाप और तोल पूरी करो और लोगों की ख़रीदी हुई चीज़ों में कमी न करो तथा धरती में उसके सुधार के पश्चात बिगाड़ न करो। यही तुम्हारे लिए उत्त्म है, यदि तुम ईमान वाले हो। तथा प्रत्येक मार्ग पर लोगों को धमकाने के लिए न बैठो और उन्हें अल्लाह की राह से न रोको, जो उसपर ईमान लाये हैं और उसे टेढ़ा न बनाओ।” (अल-आराफ़ :84-85)
फिर जब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अच्छे कर्म करने की हिदायत दी, तो उन्होंने कहा:
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍۢ○ (ھود:۹۱)
“अगर तेरे समुदाय के लोग नहीं होते, तो हम तुझे पत्थरों से मार-मार कर मार डालते, तू हम पर भारी नहीं पड़ सकता।” (हुद: 91)
ऐसा प्रतीत होता है कि मदयन वालों का बिगाड़ यह था कि वे आम तौर पर विश्वासघाती थे, उनके व्यापारिक व्यवसाय में बेईमानी बहुत बढ़ गई थी। उनके क्षेत्र से गुज़रने वाले व्यापार मार्गों पर वे डकैतियां करते थे। वे ईमान वालों को वे सत्यमार्ग से रोकते थे और वे सत्य के इतने विरोधी थे कि जब एक भले व्यक्ति ने उन्हें बुराइयों पर टोका और भलाई की ओर बुलाया, तो वे अपने बीच में उनकी उपस्थिति को सहन नहीं कर सके और उन्हें पत्थर मार-मार कर मार डालने को तैयार हो गए।
(6.) चोरी को भी फ़साद के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, जब हज़रत यूसुफ़ के भाइयों पर एक गिलास चोरी करने का आरोप लगाया गया, तो उन्होंने कहा:
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ○(یوسف : ۷۳)
“अल्लाह की क़सम! तुम जानते हो कि हम देश में बिगाड़ फैलाने नहीं आए हैं और हम चोर नहीं हैं।” (यूसुफ: 73)
(7.) राजाओं के आक्रमण से होने वाली तबाही और विजित राष्ट्रों के नैतिक पतन को भी बिगाड़ कहा गया है। इसलिए, हज़रत सुलैमान का पत्र प्राप्त करने पर, सबा की रानी ने अपने दरबारियों से कहा:
إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةًۭ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ○ (النمل :۳۴)
“वास्तव में, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसमें फ़साद भर देते हैं, उसके गणमान्य लोगों को अपमानित करते हैं और इसी तरह की हरकतें करते हैं।” (अन्नमल: 34)
कुरआन में बिगाड़ की व्यापक परिभाषा यह दी गई है, जो संबंधों और लगावों को ख़राब करता है और उन रिश्तों को नष्ट करता है, जो वास्तव में मानव सभ्यता का आधार हैं। कहा गया:
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ○ (الرعد:۲۵)
“और जो लोग अल्लाह के अहद को क़ायम करने के बाद तोड़ देते हैं, और उन बंधनों को काट देते हैं जिन्हें जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उन्हीं पर अल्लाह की धिक्कार है और वही लोग हैं. जिनके लिए बुरा ठिकाना है।” (अल-रअद :25)
(9.) शासन के उस रूप को भी बिगाड़ कहा गया है, जिसमें सत्तारूढ़ शक्ति का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के बजाय शोषण, दमन, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के लिए किया जाए। अत: कहा गया:
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ○(البقرہ :۲۰۵)
“और जब वह शासक बन जाता है, तो वह कोशिश करता है कि ज़मीन में फ़साद फैलाए और खेतों और नस्लों को तबाह करे, और अल्लाह फ़साद को पसन्द नहीं करता।” (अल-बक़राः 205)
(10.) अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए भी, बिगाड़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कहा गया:
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًۭا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ○ (النحل:۸۸)
“जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका, हम उनके द्वारा फैलाए जाने वाले फ़सादों के कारण यातना पर यातना भेजेंगे।” (अल-नहल: 88)
सूरह मायदा में फ़साद को जिन लोगों से जोड़ा गया है और जिनके बारे में कहा गया है कि ''वे धरती में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं।'' उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया हैं:
وَتَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ○ (المائدہ : ۶۲)
“और तुम उनमें से बहुतों को देखोगे गुनाह और अत्याचार की ओर दौड़ते हैं और वे हराम का माल खाने में उतावले हैं।” (अल माइदाः 62)
وَكُفْرًۭا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًۭا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ ۔ (المائدہ : ۶۴)
“और हमने क़ियामत के दिन तक के लिए उनके बीच वैमनस्य और दुश्मनी डाल दी, जब इससे यह पता चला कि “इस्म”, अर्थात वे गुनाह जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता को नष्ट करते हैं और “उदवान”, अर्थात ऐसे गुनाह जिनका बुरा प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, और रिश्वत और सूदखोरी जैसे अवैध तरीक़ों से लोगों के माल खाना और वैमनस्य और घृणा रखना और स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से शत्रुता करना और उसके लिए युद्ध की ज्वाला भड़काना, ये सभी ‘फ़साद’ के कार्य हैं।
षडयंत्र और बिगाड़ को मिटाने के लिए ईश्वरीय आदेशों पर आधारित व्यवस्था की ज़रूरत
इस व्याख्या से यह सर्वविदित हो गया कि पवित्र क़ुरआन की भाषा में फ़ितना और फ़साद का क्या अर्थ है। अब अगर हम उन सभी बुराइयों पर ग़ौर करें जिन्हें फ़ितना और फ़साद के रूप में वर्णित किया गया है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे सभी सर्वजगत के रचयिता और पालनहार से अनजान एक अन्यायपूर्ण और भ्रष्ट शासन प्रणाली से पैदा होती हैं। अगर किसी बुराई के जन्म में ऐसी शासन प्रणाली का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं भी हो, तो कम से कम उसके बने रहने में निश्चित रूप से उस प्रणाली की भूमिका होती है। पहली, बात तो यह कि ऐसी व्यवस्था अपने आप में एक फ़ितना है, क्योंकि यह शासन के वास्तविक उद्देश्य के ख़िलाफ़ है। उसकी बुराई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सभी बुराइयों का स्रोत और फ़ितना और बिगाड़ के सभी मूलों और शाखाओं का स्रोत बन जाती है। यह अल्लाह के मार्ग से रोकती है, इससे सत्य और न्याय का सिर कुचला जाता है, इससे उद्दंडों और अत्याचारियों को अपने कुकर्मों के लिए बल मिलता है। इससे वे नैतिक और सामाजिक न्याय को नष्ट कर देने वाले क़ानून लागु होते हैं। इससे दुनिया में युद्ध होता है और रक्तपात की आग भड़कती है। इससे राष्ट्रों और देशों पर आपदाएं आती हैं और यही वह चीज़ है, जिसकी शक्ति किसी न किसी रूप में हर बुराई और दुष्कर्म का स्रोत बन जाती है। इसलिए, इस्लाम ने शिक्षा दी कि ऐसी शासन व्यवस्था का संगठित संघर्ष (जिहाद) और, अगर आवश्यक हो और संभव हो, तो युद्ध के माध्यम से उन्मूलन कर दिया जाए, और उनके स्थान पर अल्लाह के नियत क़ानूनों पर आधारित एक न्यायसंगत और निष्पक्ष शासन प्रणाली स्थापित की जाए इसके कार्यकर्ता केवल वे लोग हों जो “अम्र बिल-मारूफ़ और नह्यी अनिल-मुनकर” को अपना एकमात्र उद्देश्य मानते हों। जो बड़ाई के लिए नहीं बल्कि मानवता की भलाई और अल्लाह की ख़ुशी के लिए, सत्ता की बागडोर को हाथ में लेते हैं।
पवित्र क़ुरआन उठा कर देखिये, आप जगह-जगह पाएंगे कि ज़ालिमों के अनुपालन से रोका गया है और इंसान को ताकीद की गई है कि वह असत्य और अत्याचार की पैरवी करके अपना सर्वनाश न करे। कहीं आदेश दिया गया है कि:
وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ○ (الشعراء : ۱۵۱-۱۵۲)
“और उन सीमा का उल्लंघन करने वालों के आदेश को न मानो जो ज़मीन में बिगाड़ करते हैं और सुधार नहीं करते।” (अल-शुअरा': 151-152)
कहीं कहा जाता है:
ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا○ (الکہف : ۲۸)
“और उसकी आज्ञा का पालन न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से बेख़बर कर दिया है, और मनेच्छाओं का अनुसरण करता है और जिसका आदेश अन्याय पर आधारित है।” (अल-कह्फ़: 28)
कहीं किसी राष्ट्र के विनाश का कारण यह बताया जाता है:
رُسُلَهُۥ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍۢ ٥٩ وَأُتْبِعُوا۟ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةًۭ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ (ھود :۵۹-۶۰)
“उन्होंने हर दमनकारी और सत्य के शत्रु का अनुसरण किया, इसलिए वे इस दुनिया में धिक्कारे गए और क़ियामत के दिन भी वे धिक्कारे जाएंगे।” (हुद: 59-60)
कहीं स्पष्ट कहा गया है कि किसी देश का विनाश तभी होता है जब उसका धन और शासन दुष्टों के हाथों में पड़ जाता है:
وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًۭا○ (بنی اسرائیل :۱۶)
“जब हम किसी बस्ती को बर्बाद करने का इरादा करते हैं, तो हम उसके धनी लोगों की ओर (भलाई) का आदेश देते हैं, फिर वे अवज्ञा करते हैं और बुरे काम करते हैं, फिर वह बस्ती दंड की भागी हो जाती है और हम उसे नष्ट विनष्ट कर देते हैं।” (बनी इसराईल: 16)
इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। सामाजिक जीवन में मानव नैतिकता और संस्कृति को प्रभावित करने वाले सभी कारकों (Factors) में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी कारक, शासन है। शासन व्यवस्था अगर ग़लत हो और सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में हो जो उस का उपयोग कल्याण और मानव सेवा के बजाय बिगाड़ और स्वयंसेवा के लिए करते हों, तो ऐसी स्थिति में किसी भी अच्छाई का उभरना, सुधार के किसी प्रयास का सफल होना और किसी भी प्रकार के नैतिक गुणों का फलना-फूलना कठिन हो जाता है। क्योंकि वह सरकार स्वाभाविक रूप से बुराई और बिगाड़ की संरक्षक होती है और न केवल वह स्वयं बुराई करती है, बल्कि उसकी शक्ति नैतिक बुराइयों का पोषण करती है। इसके विपरीत, अगर सरकार एक सही और न्यायपूर्ण संविधान पर आधारित हो, तो उसका उद्देश्य यह होता है कि न्याय की स्थापना हो और सरकार चलाने वाले भले, संयमी और गुणवान लोग हों, जो अपनी अपनी शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत, वर्गीय या राष्ट्रीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए न करते हों, बल्कि मानवता की भलाई के लिए करते हों, तो इसकी सुधारात्मक शक्ति का प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगा जो सीधे तौर पर सरकार से जुड़ा है, बल्कि सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन के सभी क्षेत्र इसके सद्प्रभावों को स्वीकार करेंगे। धर्म, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता, सभ्यता, विज्ञान और दूसरे सभी क्षेत्रों में सुधार का प्रदर्शन होगा। बुराई की केवल रोक-थाम ही नहीं होगी, बल्कि बुराई के स्रोत भी सूख जाएंगे। अत: वास्तव में, फ़ित्ना और बिगाड़ को मिटाने और मानव जीवन को मुनकर से मुक्त करने के लिए सबसे आवश्यक और उपयोगी उपाय यही है कि सभी भ्रष्ट सरकारों का उन्मूलन कर दिया जाए और उनके स्थान पर एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो सिद्धांत और व्यवहार दोनों आधारों पर भलाई और सदाचार पर आधारित हो।
सशस्त्र प्रितरोध का आदेश
यह दूसरा महान और गौरवशाली उद्देश्य है जिसके लिए अल्लाह ने अपने नेक बंदों को तलवार उठाने का आदेश दिया है। पहला उद्देशय यह था कि स्वयं अपनी शक्ति को क्षीण होने से बचाया जाए। दूसरा उद्देश्य यह है कि उस सुरक्षित शक्ति का उपयोग पूरी दुनिया से फ़ितना और बुराई को ख़त्म करने और बिगाड़ फैलाने वालों से बुराई की शक्ति छीन कर उन्हें अच्छाई के अधीन करने में इस्तेमाल किया जाए। यह आदेश बहुत ही कम शब्दों में इस प्रकार दिया गया है:
قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍۢ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ. (التوبه : ٢٩)
“अहले किताब में से जो लोग न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न आख़िरत के दिन पर, और न उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) ने हराम ठहराई हैं और न सच्चाई का दीन अपनाते हैं, उनसे युद्ध करो,यहां तक कि वे अपने हाथों से जिज़्या अदा करें और वे अधीनस्त होकर रहें।”
इस आयत में जिन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने का आदेश दिया गया है, उनके लक्षण यह हैं कि हालाँकि वे किताब वाले हैं, लेकिन अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और न ही वे उन चीज़ों से परहेज़ करते हैं जिन्हें ख़ुदा और ख़ुदा के रसूल ने वर्जित ठहराया है और न अल्लाह के दीन को अपना दीन बनाते हैं। इन अपराधों का यह क्रम व्यर्थ नहीं है, बल्कि इस पर विचार करने से युद्ध के आदेश का कारण स्वत: ही समझ में आ जाता है। कहा गया कि हमने उनकी ओर किताबें भेजीं जिनमें उन्हें विचार और कर्म का सही मार्ग बताया गया और उनके लिए जीवन का एक सही नियम निर्धारित किया गया। लेकिन उन्होंने उन किताबों को छोड़ दिया और अपनी राय और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपने लिए अलग-अलग धर्म और क़ानून ईजाद कर लिए जो सच्चाई के विपरीत हैं। इस विचलन के कारण एक ओर तो उनकी सोच बिगड़ गई कि अल्लाह और बदला मिलने के दिन पर उनका विश्वास न रहा, और दूसरी ओर, उनकी हरकतें भी बिगड़ गईं कि हलाल और हराम के बीच अंतर भी बाक़ी नहीं रहा। वे षडयंत्र और बिगाड़ फैलाने लगे, जिससे अल्लाह ने और उन रसूलों ने जो उनकी ओर भेजे गए थे उन्हें मना किया था।
फिर जब अल्लाह ने उनके मार्गदर्शन के लिए वही सच्चा दीन फिर से भेजा, जिसे वे खो चुके थे, तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया और अपनी पिछली गलतियों और ग़लतफ़हमियों से चिपके रहे। हालांकि अगर वे उन्हें अपना लेते,तो वे एक किताब और क़ानून से बंध जाते, जिसके द्वारा उनके विचारों और कार्यों दोनों में सुधार आ जाता और फ़ितना और फ़साद का नाम और निशान मिट जाता। अब, अगर वे सच्चे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो उन्हें आज्ञाकारी रहकर अपने ग़लत विश्वासों और प्रथाओं पर टिके रहने की स्वतंत्रता दी जा सकती है, लेकिन उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि अपने झूठे क़ानूनों को लागू करके अल्लाह की सृष्टि को बिगाड़ कर रख दें।
युद्ध का कारण और उद्देश्य
“यहां तक कि वे अपने हाथों से जिज़्या अदा करें” में इस लड़ाई का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। अगर “यहां तक कि वे इस्लाम में आ जाएं” कहा जाता, तो तलवार के बल पर उन्हें मुसलमान बनाने का लक्ष्य होता, लेकिन “यहां तक कि वे अपने हाथों से जिज़्या अदा करें” ने बता दिया कि जिज़्या देने पर उनकी सहमति लड़ाई की अंतिम सीमा है और उसके बाद, उनके जीवन और संपत्ति पर कोई हमला नहीं किया जा सकता है चाहे वे इस्लाम स्वीकार करते हैं या नहीं।
इसी वजह से ज़िम्मियों के बारे में इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि उनके जीवन और संपत्ति और सम्मान और प्रतिष्ठा को सभी हमलों से सुरक्षित रखा जाए। मुसलमानों पर उनकी रक्षा के लिए लड़ना और अपना ख़ून बहाना अनिवार्य कर दिया गया है। हज़रत अली कहते हैं:
“उन्होंने अनुबंध स्वीकार किया है कि उनका धन हमारे धन की तरह और उनका ख़ून हमारे ख़ून की तरह पवित्र हो जाए।”
“मैं वसीयत करता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल के दायित्व को इस तरह से ध्यान में रखा जाए, ज़िम्मियों के साथ किए गए समझौते को पूरा किया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ा जाए और उन पर उनकी ताक़त से बढ़कर लगान का बोझ न डाला जाए।”
अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) उनके जीवन के सम्मान पर इतना ज़ोर देते हैं कि:
“जो कोई किसी समझौते की हत्या करे तो उसे जन्नत (स्वर्ग) की सुगंध भी नसीब न होगी, हालांकि उसकी सुगंध 40 साल की दूरी तक पहुंचती है।” इस संबंध में यह कहना सही नहीं होगा कि जीवन और संपत्ति का यह सम्मान केवल समझौतों के सम्मान के कारण है, क्योंकि यह आदेश सभी ज़िम्मियों के लिए आम है और दायित्व उठाने का केवल यही एक रूप नहीं है कि उनका इस्लामी सरकार के साथ एक नियमित समझौता हो, बल्कि यह भी है कि वे बिना शर्त के ख़ुद को इस्लामी सरकार के हवाले कर दें और सरकार ख़ुद उन्हें ज़िम्मी घोषित करे। इसलिए, इस्लाम के विद्वानों ने व्याख्या की है कि अगर मुसलमान किसी देश को तलवार के बल से जीतते हैं और उसके निवासियों के साथ उनका कोई समझौता नहीं है, तो जीते हुए ग़ैर-मुस्लिमों को ज़िम्मी ही घोषित किया जाएगा और मुसलमानों का नेतृत्व उन पर जिज़्या लगाकर उन्हें अल्लाह और रसूल (सल्ल.) की ज़िम्मेदारी के तहत ले लेगा।
इससे स्पष्ट है कि युद्ध का यह आदेश किसी धार्मिक शत्रुता पर आधारित नहीं है, अन्यथा यह न होता कि आज्ञा मानने की स्थिति में जिनके साथ युद्ध करना आवश्यक हो, आज्ञा मानने के बाद, उनके जान-माल सम्माननीय हो जाएं। हालांकि, आज्ञा मानने वालों के साथ धार्मिक दुश्मनी की भड़ास निकालना आसान है। तदनुसार, यह भी उचित से बहुत दूर मालूम होता है कि इस आज्ञा का उद्देश्य केवल जिज़्या प्राप्त करना हो, क्योंकि प्रति वर्ष कुछ दिरहम के बदले में, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना कि उनकी रक्षा करने के लिए हर दुश्मन के सामने अपना सीना तान दिया जाए, किसी लालच पर आधारित नहीं हो सकता। यह बात किसी की समझ में नहीं आ सकती कि एक अवज्ञाकारी तो जिज़्या देकर अपने व्यापार, अपने व्यवसाय, अपनी विलासिता और अपने परिवार की आजीविका का आनंद ले और मुसलमान देश की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान के कष्टों को सहन करे और अपनी जान संकट में डाले। जबकि उसके पास उस अवज्ञाकारी से जिज़्या प्राप्त करने और फिर उससे सैन्य सेवा लेने की शक्ति भी हो। अतः जिज़्या की अदायगी पर युद्ध के निषेध और जिज़्या स्वीकार कर लेने पर न्याय और शांति स्थापित करने की सारी ज़िम्मेदारी लेने से यह स्पष्ट होता है कि इस युद्ध का उद्देश्य वास्तव में उन लोगों को विद्रोह और बिगाड़ से रोकना और उन्हें शांति स्थापित करने के लिए बाध्य करना है। उन पर जिज़्या के नाम का टैक्स लगाना केवल इसलिए है कि वे इस रक्षा और सुरक्षा के ख़र्च में भाग लें जो उन्हें प्रदान की जाती है।
जिज़्या की वास्तविकता
अल्लामा इब्ने तैमिया ने “यहां तक कि वे अपने हाथों से जिज़्या अदा करें” की टिप्पणी में लिखा है कि इसका मतलब केवल यह है कि वे अनुबंध का पालन करें। जैसा कि सभी सरकारों के क़ानून में टैक्स का भुगतान करते रहना वफ़ादारी का प्रमाण है, और भुगतान न करना देशद्रोह और विश्वासघात है, उसी तरह जिज़्या का भुगतान करना भी एक समझौते के पालन का प्रमाण है और भुगतान न करना समझौता भंग करने के समान है। यही कारण है कि जिज़्या केवल लड़ने योग्य पुरुषों पर ही लगाया जाता है। महिलाओं, अवयस्क बच्चों, पागलों, वृद्धों, नेत्रहीनों और अशक्त आदि को इससे छूट प्राप्त है। बदायअ अलसनायअ में है:
“अल्लाह ने केवल उन लोगों पर जिज़्या का आदेश दिया है जो लड़ाके लोग हैं। इसके लिए सामने वाले से लड़ने की क्षमता होना शर्त है। इसलिए, जिनके पास यह क्षमता नहीं है, उन्हें युद्ध और जिज़्या दोनों से छूट दी गई है।”
जिज़्या की राशि इतनी कम निर्धारित की गई है कि उसे चुकाना भारी न पड़े। इसे वसूस करने के तरीक़ों में नर्मी पर ज़ोर दिया गया है। उन्हें पीड़ा देना या दंड के माध्यम से उन पर एक असहनीय बोझ डालना जायज़ नहीं है। एक बार हज़रत उमर के पास जिज़्या की बड़ी रकम लायी गयी। उन्होंने उसे असामान्य पाया और कहा, “मुझे लगता है कि तुमने लोगों को बर्बाद कर दिया है।” वसूल करने वालों ने उत्तर दिया, “अल्लाह की क़सम, हमने इसे बहुत नर्मी से वसूल किया है।” उमर ने फिर पूछा, “बिना मारे-पीटे?” उन्होंने कहा, “बिना मारे बांधे।” तब उमर ने उस धन को ख़ज़ाने में प्रवेश करने की अनुमति दी। हज़रत अली ने एक बार एक व्यक्ति को ज़िम्मेदार नियुक्त करते हुए निर्देश दिया कि “लगान की वसूली में उन पर इतना कठोर न होना कि उन्हें अपने गधे, अपनी गाय, अपने कपड़े या अन्य चीज़ें बेचने के लिए मजबूर होना पड़े, बल्कि उनके साथ नर्मी करना।
इन बातों से यह स्पष्ट है कि ग़ैर-मुस्लिमों पर लगाया गया जिज़्या वास्तव में एक दंड नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि लोग शांति और संविधान का पालन करें, स्वेच्छा से न्याय के क़ानून का पालन करें और सामर्थ भर उस प्रशासन का ख़र्च वहन करें, जो उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है, अत्याचार और अन्याय से बचाता है, न्याय के साथ अधिकारों का वितरण करता है, मज़बूत को कमज़ोर को दमन करने से रोकता है, कमज़ोर को मज़बूत के ग़ुलाम बनने से बचाता है। और सभी विद्रोही तत्वों को नैतिकता और मानवता की सीमाओं में बांध देता है।
क़ुरआन में कई जगहों पर जंग का मक़सद और उसके फ़ायदेमंद नतीजों का जिस तरह बयान किया गया है, उससे साफ़ है कि काफ़िरों को उनके असत्य क़ानून को लागू कर फ़ितना और फ़साद पैदा करने से रोकना और उन्हें ईश्वरीय क़ानून के तहत न्याय की व्यवस्था के अधीन लाना, ही युद्ध का उद्देश्य है। कहीं युद्ध का मक़सद बतलाया गया है, “ताकि फ़ितना बाक़ी न रहे।” कहीं इसी उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार किया गया है “कि युद्ध और दंगों का ज़ोर टूट जाए।” कहीं इन शब्दों में यही अर्थ व्यक्त किया गया है कि “यह निकट है कि अल्लाह युद्ध और उपद्रव में अविश्वासियों की शक्ति को तोड़ देगा।” कहीं बयान किया जाता है कि “अवज्ञाकारियों का बोल नीचा हुआ और अल्लाह का बोल ऊंचा हो गया। तो फ़ितना का शेष न रहना, बिगाड़ का मिट जाना, असत्य के समर्थकों की शक्ति समाप्त हो जाना, अविश्वास की शैतामी शक्ति का इस हद तक टूट जाना कि वह दुनिया के अम्न-चैन को नष्ट न कर सके। अल्लाह की सृष्टि के नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास में बाधा न डाल सके। साथ ही अवज्ञाकारियों के स्वनिर्मित क़ानूनों का रद्द हो जाना और उनके स्थान पर अल्लाह के न्याय का क़ानून लागू होना। अत्याचारियों के सिवा हर किसी को शांति और स्वतंत्रता की शुभ सूचना देना, ये ही वे उद्देश्य हैं जिनका वर्णन जंग की आयतें करती हैं।
इस्लाम और साम्राज्यवाद
दुर्भाग्य से इस युग में पश्चिम के कुछ साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने दावा किया है कि वे विश्व में सभ्यता और मानवता के विकास, पिछड़े राष्ट्रों के कल्याण और शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस ज़ुबानी दावे के विपरीत उनकी हरकत यह है कि वे कमज़ोर राष्ट्रों की आज़ादी पर डाके डालते हैं और सभ्यता और मानवता के विकास के बजाय वे दुनिया से मानवता और मानवीय गरिमा की सभी विशेषताओं को एक-एक करके मिटा रहे हैं। इससे लोगों को शक हो सकता है कि कहीं इस्लाम का दावा भी ऐसा ही न हो, कि ज़ुबान पर कल्याण की जाप और हाथ में फ़ितना और फ़साद की तलवार। इस संदेह को पश्चिमी उपनिवेशवाद और इस्लामी जिहाद की बाहरी समानता और भी मज़बूत करती है, कि जिस तरह इस्लाम में सार्वभौमिक सुधार का जिहाद केवल मुसलमानों के लिए विशेष है, उसी तरह पश्चिमी उपनिवेशवादी भी सभ्यता को विश्व विस्तार के मिशन को केवल अपने राष्ट्र का अधिकार मानते हैं। हालांकि पिछली चर्चाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन इस संदेह के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है, मगर जो कुछ भी जगह बचती है उसे संदेह के लिए छोड़ने के बजाय ज्ञान और दृढ़ विश्वास से भर दिया जाए।
जैसा कि सभी जानते हैं, साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक विशेष राष्ट्र और देश के लोगों के साम्राज्य का नाम है। अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद ब्रिटेन के निवासियों के लिए विशेष है। जर्मन साम्राज्यवाद में जर्मन वासियों के सिवा किसी और का हिस्सा नहीं है। इटालियन साम्राज्यवाद में जो कुछ भी है, इटालियंस का है। जिस प्रकार विश्व के अन्य राष्ट्रों का अंग्रेज़ी, जर्मन या इटालियन हो जाना असम्भव है। अंग्रेज़ “सभ्यता-विस्तार” के नाम पर जहाँ भी जाएंगे, अंग्रेज़ी राष्ट्रीयता साथ-साथ जाएगी।
आधुनिक लोकतंत्र में यद्यपि सैद्धांतिक रूप से देश के अल्पसंख्यकों को सह-शासकों के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यवहार में देश बहुसंख्यकों के हाथों में ही होता है और अल्पसंख्यकों को या तो मार-काट कर समाप्त कर दिया जाता है या हर तरह का दबाव डाल कर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे अपनी विशिष्ट पहचान को बहुसंख्यक समुदाय के भीतर विलीन कर दें।
उच्च सरकारी पदों पर होंगे तो अंग्रेज़ होंगे, राजनीति संघों के अध्यक्ष होंगे तो अंग्रेज़ होंगे, सत्ता और राजनीति के मालिक होंगे तो अंग्रेज़ होंगे, अन्य जातियों और राष्ट्र के लोग चाहे अंग्रेज़ी सभ्यता में कितनी भी तरक़्क़ी क्यों न कर लें, अंग्रेजों के राज्य में सत्ता और अधिकार प्राप्त होना उनके लिए बिल्कुल असंभव है। यही हाल अन्य देशों के साम्राज्यवाद का भी है। ऐसी व्यवस्था में शासन करने का अधिकार अनिवार्य रूप से एक देश के निवासियों और एक जाति के सदस्यों के लिए विशेष हो जाता है। स्पष्ट है कि जाति और राष्ट्रीयता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई व्यक्ति अपनी पसंद से अपना सकता हो। इसका दायरा उन लोगों तक ही सीमित है, जिन्हें प्रकृति किसी ख़ास जाति और देश में पैदा करना पसंद करती है। इसलिए, साम्राज्यवाद की इस प्रणाली का दरवाज़ा दूसरी जाति और दूसरे देश के लोगों के लिए हमेशा बंद रहता है। किसी राष्ट्र के साम्राज्य में अन्य राष्ट्र का केवल इसलिए कोई हिस्सा नहीं हो सकता है कि वह शासक राष्ट्र की जाति से नहीं है। फिर इसी से अन्य ख़राबियां पैदा होती हैं, शासित जाति एक समुदाय के रूप में अपमानित हो जाती है, उसमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की भावना बाक़ी नहीं रहती। अगर उसके शासक दमन और अत्याचार के ताथ शासन न करें तब भी उसमें हीनता और दीनता स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है, जो एक समय तक स्वशासन से वंचित रहने का अपरिहार्य परिणाम है और आध्यात्मिक विकास के लिए घातक कीटाणु है।
इसके विपरीत, इस्लाम किसी जाति या राष्ट्र या मातृभूमि का नाम नहीं है। यह एक सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसके दरवाज़े सभी के लिए खुले हैं। अरबी, ग़ैरअरब, अबीसीनियन, चीनी, हिन्दी, यूरोपीय, सभी इसे अपना सकते हैं और इसे अपनाने के बाद इसकी सामूहिक व्यवस्था में सबके अधिकार, शक्तियाँ और पद एक समान घोषित किये जाते हैं। इसका किसी व्यक्ति की जाति या रंग या राष्ट्रीयता से कोई लेना-देना नहीं है। यह मनुष्य को केवल एक मनुष्य के रूप में संबोधित करता है और उसके सामने जीने का शुद्ध तरीक़ा रखता है। जो कोई भी इस विधि और क़ानून को अपनाता है वह इस्लामी जमाअत का सदस्य है, इस्लामी शासन में बराबर का भागीदार है, और उसकी व्यक्तिगत क्षमता उसे ख़लीफ़ा और इमाम के पद तक पहुंचा सकती है। जिस प्रकार संसार की सरकारों में नेतृत्व की पात्रता का मानक सिविल सेवा या इसी प्रकार की अन्य किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसी प्रकार इस्लामी प्रशासन में नेतृत्व की योग्यता का मानक इस्लामी सिद्धांतों और जीवन व्यवस्था को अपनाना और इसके क़ानूनों का पालन करना है। अगर एक एबिसिनियन ग़ुलाम है, तो उसे कुलीन अरबों पर शासन करने से कोई नहीं रोक सकता। नबी (सल्ल.) का स्पष्ट फ़रमान है:
“उसकी सुनो और उसका आदेश मानो, चाहे तुम्हारे ऊपर एक गंजा अबीसीनियन ग़ुलाम शासक बना दिया जाए।”
इस्लाम का आखिरी आह्वान अरब से उठा। अरबों को ही इसका झंडा ऊंचा उठाने का सौभाग्य प्राप्त है। मगर उसने कभी भी शासन और नेतृत्व को अरबों के लिए विशेष नहीं किया। जब तक अरब “योग्य” रहे, उन्होंने आधी दुनिया पर शासन किया, जब उनमें योग्यता नहीं रही, तो अरबों द्वारा जीते गए ग़ैरअरब इस्लामी राज्य के उत्तराधिकारी बन गए और उन्होंने स्वयं अरबों पर शासन किया। तुर्क इस्लाम के घोर शत्रु थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम के दायरे में प्रवेश किया, तो आधे से अधिक इस्लामी दुनिया ने उन्हें अपने शासकों के रूप में स्वीकार कर लिया और चांगाम से क़रतबा तक उनके शासन के झंडे लहराने लगे। हम मानते हैं कि आज मुस्लिम देशों में राष्ट्रीयता और नस्ल का भेदभाव बहुत आम है, लेकिन इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। इस्लाम ने अपनी किसी भी शिक्षा और अपने किसी आदेश में इस भेद को रत्ती भर भी स्थान नहीं दिया है।
यह तो इस्लाम और साम्राज्यवाद के बीच का बाहरी अंतर था। आंतरिक अंतर इससे भी अधिक स्पषट है। साम्राज्यवाद वास्तव में एक राष्ट्र की अपने राज्य का विस्तार करने और धन प्राप्त करने की इच्छा का नाम है। जब कोई राष्ट्र अपने देश में प्राप्त धन और सरकार से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह अन्य देशों पर आक्रमण करता है और उनकी संपत्ति को ज़ब्त कर लेता है, अपने निवासियों को अपनी प्रजा और दास बना लेता है, और उनके ख़र्च पर अपने उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देता है। यह काम पहले भी किया जाता था और हमेशा उपद्वी लोगों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन अब पश्चिमी देशों ने इस जमीन हड़पने और लूटपाट को पहली बार “सभ्यता” का नाम दे दिया है कि “शक्ति सत्य है” और कमज़ोर दुनिया को जीने का कोई अधिकार नहीं। कमज़ोर राष्ट्रों के बीच “सभ्यता के प्रसार” का उन्होंने जो तरीक़ा ईजाद किया है, वह उन्हें अज्ञानता, गरीबी, धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है और दुनिया की शांति और व्यवस्था को नष्ट कर देती है।
इस्लाम की पवित्र शिक्षा साम्राज्यवाद के इस दोष से मुक्त है। बल्कि, इसके विपरीत, वह मानव जाति को ऐसी विद्रोही ताक़तों को मिटाने और उनके स्थान पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता है। उसका दावा है कि हुकूमत और बादशाहत केवल अल्लाह के लिए है, अल्लाह के बंदों को यह हक़ नहीं है कि अल्लाह के ग़ुलामों को अपना ग़ुलाम बना लें। उन का काम केवल यह है कि अल्लाह के ख़लीफ़ा के रूप में उसके बन्दों की सेवा और कल्याण के काम करें और जो ताक़त उसे प्राप्त है उसका इस्तेमाल अल्लाह के बन्दों की भलाई के लिए करें :
وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۔ (النور: ۵۵)
“तुम्हारे बीच जो लोग ईमान लाए और तद्नुसार कर्म करते रहे उन से अल्लाह ने वादा किया है कि उन्हें ज़मीन में इस तरह अपना ख़लीफ़ा बनाएगा जिस तरह उनसे पहले के लोगों को बनाया था।”(अल-नूर: 55)
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ . إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغًۭا لِّقَوْمٍ عَـٰبِدِينَ○ (الانبیاء : ۱۰۵-۱۰۶)
“और हमने “ज़बूर” में नसीहत के बाद लिख दिया है कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बन्दे होंगे। इसमें अल्लाह के आदेश मानने वाले राष्ट्रों के लिए एक संदेश है।”
ये ख़िलाफ़त और दुनिया की विरासत पाने वालों को ज़ोर देकर बता दिया जाता है कि ख़ुदा के बन्दों पर जो वर्चस्व तुमको दिया गया है, वह अल्लाह की अमानत है, इसे अपनी निजी सम्पत्ति समझ कर मनेच्छाओं की पूर्ति में ख़र्च मत करना। जब हज़रत दाऊद को राज्य दिया गया, तो कहा गया:
يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ○(ص: ۲۶)
“ऐ दाऊद! हमने तुमको ज़मीन में अपना प्रतिनिधि बनाया है, अत: सच्चाई और ईमानदारी के साथ शासन करो और मनेच्छाओं के पीछे न चलो, क्योंकि मनेच्छाएं तुम्हें ख़ुदा के रास्ते ते भटका देंगी। जो लोग ख़ुदा के रास्ते से हट जाते हैं, उनके लिए कड़ी यातना है, क्योंकि वे उस दिन को भूल गए जब उनके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा।” (साद :26)
सत्ता मिलने के बाद व्यक्ति में सबसे बड़ा अवगुण यह आ जाता है कि वह अपने आप को सामान्य लोगों से ऊंचा समझने लगता है और अपनी वास्तविकता को भूल जाता है और इस भ्रम में पड़ जाता है कि जो लोग उसके अधीन हैं वे उसकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इस्लाम इस दोष के बचने पर बहुत ज़ोर देता है और मुक्ति की प्राप्ति को उससे बचने पर निर्भर ठहराता है:
تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًۭا ۚ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○(قصص :۸۳)
“यह परलोक का इनाम (स्वर्ग) है, हम इसे उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, जो धरती में बड़ाई उपद्रव नहीं करते। आख़िरत के अच्छे परिणाम केवल अज्ञाकारियों के लिए हैं।” (क़सस:83)
सरकार स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है। न्याय केवल दो परस्पर विरोधी दलों के बीच सही निर्णय लेने का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक न्याय यह है कि शासक अपनी शासित के साथ व्यवहार करने में सत्य का पालन करे। यहां तक कि जहां उसके व्यक्तिगत लाभ और सत्ता का सवाल हो, वहां भी शक्ति और अधिकार रखने के बावजूद, वही निर्णय ले जो सत्य हो, चाहे इसका नुक़सान स्वयं उसको पहुंचे या उसके परिजनों और प्रियजनों को। इस्लाम इसी न्याय की शिक्षा देता है:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًۭا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا○ (النساء :۱۳۵)
“ऐ ईमान वालो! न्याय के साथ खड़े रहकर अल्लाह के लिए साक्षी बन जाओ। चाहे यह साक्ष्य तुम्हारे अपने अथवा माता पिता और समीपवर्तियों के विरुध्द ही हो। पहुंच वालों के समर्थन अथवा निर्धन के लिए सहानुभूति की भावना तुम्हें सच्ची गवाही और न्याय से न फेर दे, क्योंकि अल्लाह उन दोनों का तुमसे अधिक हितैषी है। अतः अपनी मनेच्छाओं के लिए न्याय से न फिरो। यदि तुम बात घुमा फिरा कर करोगे अथवा गवाही देने से कतराओगे, तो जो तुम करते हो, निःसंदेह अल्लाह उससे सूचित है।” (अल-निसा: 135)
इससे भी आगे बढ़कर, वह आदेश देता है कि जिनसे तुम्हारी शत्रुता है उन के साथ भी न्याय करो:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ○ (المائدہ :۸)
“किसी जाति की शत्रुता तुम्हें उसके साथ न्याय न करने के लिए विवश न करे। न्याय करो, क्योंकि यही धर्मपरायणता के अधिक निकट है।” (अल-मायदा :8)
ताक़त और शक्ति प्राप्त करने के बाद, एक राष्ट्र में अनिवार्य रूप से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और कमज़ोर राष्ट्रों की भूमि छीन लेने की इच्छा विकसित हो जाती है। यही देश और धन का लोभ है जो क्रूरता और उपद्रव का वास्तविक आधार है और इसी कारण समुदायों के बीच युद्ध हुआ करते हैं। इस्लाम इसकी कड़ी निंदा करता है और इससे केवल परहेज़ करने का ही आदेश नहीं देता है, बल्कि इस अपराध को करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद छेड़ने का आदेश देता है, जैसा कि फ़ितना और फ़साद के अध्ययन में बताया जा चुका है। एक हदीस में, पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा:
“जिसने एक बालिश्त ज़मीन भी जुल्म करके हासिल की, अल्लाह क़ियामत के दिन उसके गले में इस जैसी सात ज़मीनों का फंदा लटकाएगा।” (मुस्लिम)
एक अन्य हदीस में है:
“यह धन और सम्पत्ति आनंद देने वाली चीज़ है। जिसने इसे सत्य के साथ कमाया और सत्य के स्थान पर व्यय किया, उसके लिए तो यह उत्तम पाथेय है। परन्तु जिसने इसे बिना अधिकार के प्राप्त किया वह उस मनुष्य के समान है जो खाता तो है, परन्तु तृप्त नहीं होता।”
इस्लाम ने सत्ता के उन सभी सुखों को हराम (वर्जित) ठहरा दिया है, जिस के लोभ में मनुष्य उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस्लाम का शासक न तो प्रजा के आम लोगों से अलग कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, न ही वह महानता और गरिमा के सिंहासन पर बैठ सकता है, न ही वह अपने सामने किसी की गर्दन झुकवा सकता है, और न ही वह सत्य के क़ानून के ख़िलाफ़ एक पत्ता भी हिला सकता है। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपने प्रियजनों या मित्रों या स्वयं अपने आप को आम आदमी की जायज माँगों से बचा सके। न ही वह सत्य के विरुद्ध भूमि का एक टुकड़ा या कोई उपहार ले सकता है, और न ही वह भूमि के एक टुकड़े को ज़ब्त कर सकता है। उसे हमेशा यह डर लगा रहता है कि उसके कर्मों का गंभीर हिसाब लिया जाएगा। अगर हराम (निषिद्ध) का एक पैसा, ज़बरदस्ती ली गई ज़मीन का एक टुकड़ा, अहंकार और घमंड का एक अंश, क्रूरता और अन्याय का एक कण और स्वार्थ का संदेह भी उसके खाते में निकल आया तो उसे कठोर दण्ड भुगतना पड़ेगा।
हज़रत अबू बक्र ने ख़लीफ़ा चुने जाने के बाद अपने उपदेश में इस्लाम में शासन और शासक की वास्तविक स्थिति और उनकी आधिकारिक ज़िम्मेदारियों की सही स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है:
“लोगो! मुझे तुम्हारे शासन का काम सौंपा गया है, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। मेरे लिए सबसे कमज़ोर आदमी तब तक सबसे मज़बूत है जब तक मैं उसे उसका अधिकार न दिलवा दूं, और मज़बूत व्यक्ति सबसे कमज़ोर है, जब तक मैं उससे अधिकार न वसूल कर लूं। लोगो! मेरी स्थिति तुम्हारे एक सामान्य व्यक्ति से अधिक नहीं है। अगर तुम मुझे सीधे मार्ग पर चलते देखो, तो मेरा अनुसरण करो और अगर तुम मुझे भटका हुआ देखो, तो मुझे सीधा कर दो।”
इस प्रकार हर प्रकार के भव्य आडंबर, प्रभुता निरंकुशता, धन की प्रचुरता और स्वयं के सभी सुख-सुविधाओं को हटा देने के बाद सरकार के उत्तरदायित्वों का शुष्क और स्वादहीन भाग जो शेष रह जाता है वह स्वयं इस्लाम की भाषा में यह है:
ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ۔ (الحج: ۴۱)
“अगर हम उन्हें ज़मीन में सत्ता दें तो वे नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, भलाई का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।” (अल-हज्ज: 41)
यह इस्लाम का सिर्फ़ दावा ही नहीं है, बल्कि इस्लाम के पैग़म्बर और उन के सच्चे ख़लीफ़ाओं ने इसका पूरा व्यवहारिक नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। इस किताब का विषय न क़ानून की व्याख्या है और न इतिहास की पड़ताल, फिर भी हम कुछ उदाहरण देकर यह बताएंगे कि इस्लामी शासन का आदर्श क्या है?
बनी मख़ज़ूम की एक सम्मानित महिला फ़ातिमा बिन्त असद चोरी के आरोप में गिरफ़्तार होकर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के पास आती है। क़ुरैश को डर है कि कहीं वे अन्य सामान्य लोगों की तरह उसका हाथ काटने का भी आदेश न दे दें। सिफ़ारिश के लिए लोग उनके सबसे प्रिय पात्र ओसामा बिन ज़ैद को भेजते हैं। नबी उनकी सिफ़ारिश को यह कहकर ख़ारिज कर देते हैं कि तुम से पहले के लोग इसी वजह से मिट गए कि वे कम दर्जे के लोगों पर दंड का आदेश जारी करते थे और सम्मानित लोगों को छोड़ देते थे। फिर वे जोश में आकर कहते हैं:
“उस सत्ता की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुहम्मद (अल्लाह के रसूल) की बेटी फ़ातिमा ने चोरी की होती, तो मैं उसका भी हाथ काट देता।” (बुख़ारी और इब्ने माजा)
बद्र की लड़ाई में, क़ुरैश के अन्य सरदारों के साथ, ख़ुद पैग़म्बर (सल्ल.) के दामाद (अबुल-आस) को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्हें आम क़ैदियों की तरह बंद कर दिया गया है। उनके पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आदेश दिया जाता है कि घर से पैसे मंगवा कर दें अन्यथा जेल में रहें। वह अपनी पत्नी, अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की बेटी, ज़ैनब को एक संदेश भेजते हैं, और उनके पास से पति के लिए फिरौती के रूप में एक क़ीमती हार आता है, जिसे अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की पत्नी हज़रत ख़दीजा ने दहेज के रूप में दिया था। हार को देखकर नबी को अपनी जीवन साथी की याद आ जाती है और बेक़ाबू आंसू निकल आते हैं। फिर भी वे अपने अधिकार से फिरौती को माफ़ नहीं करते हैं। वे आम मुसलमानों से इजाज़त माँगतें हैं कि अगर इजाज़त हो तो बेटी को उसकी माँ की यादगार वापस लौटा दी जाए। जब आम मुसलमान इजाज़त दे देते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अपने दामाद को फिरौती के बिना आज़ाद कर दिया जाता है। (तबरी, अबू दाऊद)
हुदैबियाह के स्थान पर अल्लाह के दूत और क़ुरैश के बीच समझौता होता है। शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और समझौते को लिखा जा रहा है। ठीक उस स्थिति में, एक मुस्लिम, अबू जुंदाल बिन सुहैल, क़ुरैश की क़ैद से भाग आते हैं। उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, बदन पर इतने घाव हैं कि आते ही मुसलमानों के सामने गिर जाते हैं और कहते हैं, “अल्लाह के लिए, मुझे उनकी क़ैद से बाहर निकालो।” अल्लाह के रसूल की रकाब में तलवार से लैस 1400 मुसलमान हैं, और अबू जुंदाल को एक इशारे पर रिहाई मिल सकती है, लेकिन क़ुरैश ने एक शर्त रखी है कि “क़ुरैश में से जो भी मुसलमानों के पास जाएगा, उसे वापस कर दिया जाएगा।” “और मुसलमानों में से जो मक्का जाएगा वह वापस नहीं आएगा।” इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपना सहारा देने से इनकार कर दिया। वे अपने घाव दिखाते हैं और चिल्लाते हैं, “क्या आप मुझे इसी क्रूरता का निशाना बनने के लिए वापस करने जा रहे हैं?” मगर वे कहते हैं:
“अबू जुंदाल! सब्र रखो और संयम से काम लो। हम वचनभंग नहीं कर सकते। अल्लाह तुम्हें छुड़ाने का कोई रास्ता निकालेगा।”
यरमूक के युद्ध के अवसर पर, रोम का सीज़र मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाखों की सेना इकट्ठा करता है और मुसलमानों को सीरिया और फ़िलिस्तीन से बाहर निकालने और उनकी शक्ति को कुचलने का संकल्प लेता है। उस फैसले की घड़ी में मुसलमानों को अपनी ताक़त बचाने के लिए एक-एक पैसे की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद वे हमस के निवासियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे प्राप्त टैक्स यह कहते हुए लौटा देते हैं कि अब हम तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए अब तुम अपनी व्यवस्था कर लो। इस पर हमस के लोग कहते हैं कि आपका न्याय हमें उस अत्याचार और अन्याय से अधिक प्रिय है, जिससे हम पहले पीड़ित थे। हम आपके नेता के नेतृत्व में हर सेना के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यह याद रखना चाहिए कि हरकुलिस एक ईसाई राजा था और जो लोग अपने मुस्लिम शासकों की ओर से उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते थे, वे ईसाई थे और सदियों से रोमन साम्राज्य द्वारा शासित थे।
हज़रत उमर के बेटे अबू शाहमा ने शराब पी ली तो उन्हें एक आम अपराधी की तरह गिरफ़्तार कर लिया गया, हज़रत उमर ने ख़ुद उन्हें अपने हाथों से 80 कोड़े मारे और इन कोड़ों के सदमे से उनकी मौत हो गई।
फ़ारस के क्षेत्र में मुसलमान एक शहर (शाहरियाज) को घेर लेते हैं और घेर लिए गए लोगों का प्रतिरोध इस हद तक कमज़ोर हो जाता है कि शहर की जीत बिल्कुल निश्चित हो जाती है। इसी बीच इस्लामी सेना का एक ग़ुलाम युद्धविराम का एक पत्र लिखता है और उसे एक तीर से बांधकर शहर में फेंक देता है। दूसरे दिन जब इस्लामी सेना शहर पर हमला करना चाहती है तो शहर के लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और बाहर निकल कर कहते हैं कि एक मुसलमान ने हमें शांति दी है। शांतिपत्र देखा जाता है, तो वह किसी दास द्वारा लिखित होता है। इस मामले में हज़रत उमर से पूछा जाता है कि इस शांतिपत्र का क्या मूल्य है। इसके जवाब में वे लिखते हैं, “मुस्लिम ग़ुलाम भी आम मुसलमानों की तरह है। उसके दायित्व का वही मूल्य है जो सामान्य मुसलमानों के दायित्व का है, इसलिए उसके द्वारा दिए गए आदेश को लागू किया जाए।
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की मृत्यु के बाद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक को अरब साम्राज्य के ख़लीफ़ा (शासक) के रूप में चुना जाता है। चुनाव के दूसरे दिन, हज़रत उमर देखते हैं कि अबू बक्र सिर पर कपड़े का थान लादे बाज़ार जा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा, “अब आप मुसलमानों के अमीर हैं, यह काम आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने जवाब दिया,” फिर मैं अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? हज़रत उमर ने सुझाव दिया कि अबू उबैदा आपके लिए यह काम करेंगे। अत: उनके साथ इस्लामी दुनिया के ख़लीफ़ा का मामला तय हो जाता है कि वे उनका व्यवसाय संभालेंगे और उनके परिवार के लिए एक सामान्य दर्जे के निवासी का खाना और गर्मी सर्दी के कपड़े उपलब्ध करा दिया करें। फिर बैतुलमाल (राजकोष) से खलीफ़ा के लिए 500 दिरहम (आज (1927 ई.) की गणना के अनुसार सौ रुपये से थोड़ा अधिक और आज, 2023 की गणना के अनुसार लगभग 10 हज़ार) का मासिक वेतन तय कर दिया गया। जब मौत का समय निकट आया तो लोगों से बोले कि ख़लीफ़ा होने के बाद मेरे माल में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसकी गणना करना और इसे नए ख़लीफ़ा को सौंप देना। इसलिए जब मौत के बाद हिसाब लगाया जाता है तो एक ऊंट, एक ग़ुलाम और एक पुरानी चादर के सिवा कुछ नहीं निकला।
हज़रत उमर के समय में इस्लामी विजय की बाढ़ ईरान से उत्तरी अफ्रीका तक फैल गई। विजयधन और लगान की इतनी अधिक संपत्ति थी कि हर साल करोड़ों दिरहम राजकोष में डाले जाते थे। सीजर और कसरा के सारे ख़ज़ाने मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गए। लेकिन ख़ुद इस राज्य के शासक के शरीर पर बारह पैबंद लगे कपड़े थे। पांव में फटी हुई चप्पल, और सिर पर पुरानी पगड़ी बांधकर वे विधवाओं, अनाथों और ज़रूरतमंदों को ख़बरगीरी करते फिरते थे। जब रोम और दूसरे इलाक़ों के लोग आते तो उनके लिए आम मुसलमानों में ख़लीफ़ा को पहचानना मुश्किल हो जाता। जब सीरिया की यात्रा की, तो इस तरह कि लोग इस्लाम के ख़लीफ़ा और उसके ग़ुलाम के बीच अंतर नहीं कर सके। बैतुल-मकदिस की जीत के मौक़े पर जब उन्होंने शहर में प्रवेश किया, तो वे पैदल चल रहे थे और इतने मोटे कपड़े पहने हुए थे कि ईसाइयों के दास भी नहीं पहनते थे। ऊंट का दूध, ज़ैतून का तेल, सिरका और गेहूं की रोटी, ये सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ थे जो उन्हें उपलब्ध था। जब उनकी मृत्यु हुई, तो घर में क़र्ज़ चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, इसलिए आवास बेच दिया गया और क़र्ज़ चुका दिया गया।
ये घटनाएँ क़िस्सा और कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के प्रामाणिक तथ्य हैं। उन्हें देखिए और बताइए कि दुनिया में इससे बेहतर शासन की कोई और मिसाल है? जिन लोगों का संविधान इस पवित्रता पर आधारित है, यह अल्लाह का भय, यह निःस्वार्थता, यह स्वतंत्रता और समानता, यह न्याय और निष्पक्षता, यह समझौता के प्रति निष्ठा और यह ईमानदारी और विश्वास, क्या उनका यह दावा झूठा है कि दुनिया पर शासन करना या अधिक सही शबदों में कहें तो दुनिया की सेवा करना उनका अधिकार है। अगर उन्होंने रोम के अत्याचारी और क्रूर शासकों से रोम के सिंहासन को ख़ाली करा लिया, अगर उन्होंने आसपास की सभी शैतानी शासकों के सिंहासनों को उखाड़ फेंका। उसकी जगह न्याय पर आधारित सतकार स्थापित की, तो क्या यह मानवता के प्रति क्रूरता थी, या उसकी सेवा? उनकी तुलना में पश्चिम के इन झूठे दावेदारों का क्या मूल्य, जिनका धर्म-परायणता से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने अपने वादे निभाने के बारे में सोचा ही नहीं, न्याय और निष्पक्षता, ईमानदारी और भरोसे से उनका कोई संबंध नहीं है। ये केवल देश पर क़ब्ज़ा करने के लालची हैं, धन सम्पत्ति का लोभ और सत्ता की लालसा के सिवा वे किसी ओर भावना से परिचित नहीं है?
हम मानते हैं कि बाद के ज़मानों में अधिकांश मुस्लिम शासकों का चलन इस्लाम द्वारा प्रस्तुत मूल विश्वदृष्टि के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन इसमें दोष इस्लाम का नहीं उसके मानने वालों का है। इस्लाम क़ुरआन और पैग़म्बर (सल्ल.) की सुन्नत से लिया गया क़ानून है। जो शासन इस क़ानून के अनुसार काम करता है वह इस्लामी शासन है और जो इसके ख़िलाफ़ काम करता है वह इस्लामी शासन नहीं है। हमारे लिए मुस्लिम बादशाहों की कार्रवाई प्रमाण नहीं है, बल्कि इस्लाम का क़ानून प्रमाण है। अगर उसमें कोई दोष है तो उसे प्रस्तुत किया जाए।
इस्लामी विजयों का वास्तविक कारण
अगली चर्चा शुरू करने से पहले, यहाँ एक और मुद्दे को स्पष्ट कर देना ज़रूरी है। इस किताब में बार-बार कहा गया है और आगे भी जगह-जगह इस बात का उल्लेख होगा कि इस्लामी शरीयत में राज्य को हथियाने के मक़सद से तलवार उठाना बिल्कुल हराम (वर्जित) है। इससे यह प्रश्न उठता है कि जब यह कार्य हराम है तो सहाबा (नबी सल्ल. के साथियों) और ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन (सच्चे ख़लीफाओं : अर्थात पहले चार ख़लीफ़ा – हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली) के हमलों का क्या औचित्य होगा, जो उन्होंने इराक़, सीरिया, ईरान, अर्मेनिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका आदि देशों पर किये? इस्लाम विरोधियों ने बड़ी शिद्दत से यह आपत्ति उठाई है। और मुस्लिम इतिहासकारों और लेखकों ने इसका बहुत विस्तृत उत्तर भी दिया है, लेकिन किसी ने भी इस पर विचार नहीं किया कि इस मामले में इस्लाम और ग़ैर-मुस्लिमों के दृष्टिकोण में गंभीर अंतर है। इसलिए, जिन लोगों ने ग़ैर-मुस्लिमों के दृष्टिकोण को सामने रखकर जवाब दिया है, उन्होंने इस्लाम की ग़लत व्याख्या की, और जिन्होंने इससे बेपरवाह होकर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने और अधिक संदेह पैदा कर दिए हैं।
तथ्य यह है कि इस्लाम शासन के मामले में “राष्ट्रीय” और “विदेशी” के बीच कोई अंतर नहीं करता है, बल्कि “न्याय” और “अत्याचार” को भेद का कारण ठहराता है। अगर किसी देश की सरकार उसके अपने नागरिकों के हाथों में है लेकिन उसके शासक दुष्ट, चरित्रहीन, उत्पीड़क, स्वार्थी और निर्दयी हैं, तो इस्लाम की दृष्टि में वे उतने ही घृणित हैं जितना कि एक विदेशी सरकार के ऐसे चरित्रहीन लोग हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई विदेशी अरब पर शासन करता है और सभी मामलों में न्याय, विश्वास, ईमानदारी और अल्लाह से डरते हुए काम करता है, वह उत्पीड़ितों की देखभाल करता है, उन्हें उनके अधिकार दिलाता है, घमंड और अहंकार नहीं दिखाता है, निजी स्वार्थ से बचता है और जनता के कल्याण के अलावा किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, तो वह इस अरब शासक से बेहतर है, जो इन गुणों से ख़ाली है।
यह विचार कि एक अत्याचारी अरब अरबों के लिए एक विदेशी की तुलना में बेहतर है, और कोई तुर्क कितना भी अच्छा और धर्मपरायण क्यों न हो, लेकिन केवल इसलिए कि वह एक तुर्क है, इराक़ी उसे स्वीकार नहीं कर सकते, यह एक ऐसा विचार है जिसे इस्लाम पूरी तरह से असत्य मानता है। वह इस मामले को "राष्ट्रीयता” और “देशभक्ति" की दृष्टि से नहीं बल्कि शुद्ध "मानवता" की दृष्टि से देखता हैं। उसका विश्वास है कि एक भला और सज्जन व्यक्ति हर हाल में एक दुर्जन व्यक्ति से बेहतर है। मानव गुणों में अपने और पराए, देशी और विदेशी, भारतीय और इराक़ी, काले और गोरे के बीच अंतर करना अंधा पूर्वाग्रह है।
इस्लाम की इस मान्यता के अनुसार, शासन की गुणवत्ता न तो उसका राष्ट्रीय और स्वशासित होना है और न ही उसकी बुराई विदेशी और परशासित होना है। एकमात्र वास्तविक प्रश्न यह है कि सरकार की व्यवस्था निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है या नहीं। अगर यह यह स्थिति है, तो इस्लाम उस को मिटाने की कोशिश तो परे ऐसे इरादे को भी गुनाह और बड़ा अन्याय मानता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस्लाम अन्यायपूर्ण और क्रूर शासन व्यवस्था को मिटाकर उसकी जगह सत्य और न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित करना ही अपना पहला दायित्व समझता है। इसका अर्थ यह है कि उसके लिए शासन के अच्छे या बुरे होने के प्रश्न का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि यह राष्ट्रीय है या नहीं। दूसरी बात यह है कि ग़ैर-राष्ट्रीय सरकार आमतौर पर क्रूर और दमनकारी होती है, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क़ब्ज़ा ही इस लिए करता है ताकि उसे ग़ुलाम बनाया जा सके और उसका शोषण अपने लाभ के लिए किया जा सके। इसके विपरीत, राष्ट्रीय सरकार में सुधार की योग्यता अधिक होती है। लेकिन इसके बावजूद यह ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय सरकार हर हाल बेहतर हो और ग़ैर-राष्ट्रीय सरकार हर हाल में अन्यायपूर्ण हो। यह संभव है कि एक राष्ट्र पर ख़ुद उसी के उद्दंड और उपद्रवी लोगों का शासन हो जाए और वे उसे अपने स्वार्थी लक्ष्यों का ग़ुलाम बनाकर नष्ट कर दें। इसी प्रकार यह भी संभव है कि किसी राष्ट्र को विदेशी राष्ट्र के निःस्वार्थ और सुधारवादी लोग आकर अत्याचार के चंगुल से मुक्त कराएं और उसके लिए भौतिक और नैतिक विकास का मार्ग खोल दें। इसलिए, शासन की अच्छाई की असली कसौटी उसका न्यायपूर्ण और कल्याणकारी होना है, और उसकी बुराई की असली कसौटी उसका अन्यायी और अत्याचारी होना है।
इससे यह अर्थ निकालना उचित नहीं है कि इस्लाम राष्ट्रीय शासन का विरोधी है। वह प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार को स्वीकार करता है कि वह अपनी स्थिति में ख़ुद सुधार करे। लेकिन जब किसी राष्ट्र के कर्म बिगड़ जाएं, उसकी नैतिक स्थिति बिगड़ जाए, और वह अपने दुष्ट और भ्रष्ट लोगों का अनुसरण करके अपमान की गहराई में गिर जाए, तो इस्लाम के अनुसार, उस राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार नहीं रहता है। और दूसरे लोगों को जो उससे बेहतर हैं उस पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अवज्ञाकारी और दुष्ट राष्ट्रों को पवित्र क़ुरआन में कई स्थानों पर यह धमकी दी गई है कि:
وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَـٰلَكُم○ (محمد:۳۸)
“अगर तुम सच्चाई से मुंह फेरोगे, तो अल्लाह तुम्हारे स्थान पर दूसरे लोगों को खड़ा करेगा और वे तुम जैसे नहीं होंगे।” ( मुहम्मद :38)
إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًۭٔا ۗ۔ (التوبہ :۳۹)
“अगर तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें कष्टदायक यातना देगा और तुम्हारे स्थान पर एक और समुदाय खड़ा कर देगा और तुम उसका कुछ बिगाड़ न सकोगे।” (अल-तौबा: 39)
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ۔ (النساء : ۱۳۳)
“लोगो! अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारे स्थान पर अन्य लोगों को ले आए।” (अल-निसा ': 133)
क़ुरआन में इस अर्थ की कई आयतें हैं और उन सभी का मक़सद यह है कि सरकार और बादशाहत का अधिकार क्षमता के साथ जुड़ा है, एक राष्ट्र जब यह क्षमता खो देता है वह इस अधिकार को भी खो देता है और जो राष्ट्र यह क्षमता अपने भीतर विकसित कर लेता है, वह यह अधिकार भी प्राप्त कर लेता है। इस क्षमता को केवल शक्ति और बल का पर्याय नहीं समझना चाहिए। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए विशेष है जो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, अच्छे कामों का आदेश देते हैं, हर अच्छे काम को करने में दृढ़ रहते हैं और मानते हैं कि एक दिन उन्हें अपने कामों का पूरा लेखा-जोखा प्रसतुत करना होगा और उसी के आधार पर उन्हें प्रतिफल मिलेगा।
ये भले लोग किसी समुदाय या किसी देश की संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे समस्त मानव जाति और समस्त मानव जगत के सामान्य धरोहर हैं। आदम की सभी संतानों को उनकी क्षमता से लाभ उठाने का अधिकार है। और अगर वे अनावश्यक रूप से एक सीमित समूह या क्षेत्र के लिए अपनी सेवाएं आरक्षित करते हैं, तो यह निश्चित रूप से मानवता के प्रति उनका अन्याय होगा। इस्लाम ने उनके लिए रंग या नस्ल या भौगोलिक वितरण जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, बल्कि बिना किसी प्रतिबंध के उनकी क्षमताओं के लाभों को ज़मीन के सभी क्षेत्र के लिए सामान्य बना दिया है। इसलिए, पवित्र क़ुरआन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है:
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ○ (الانبیاء ۱۰۵)
“हमने ज़बूर में चेतावनी के बाद लिखा है कि” ज़मीन “के उत्तराधिकारी हमारे नेक बन्दे होंगे।” (अल-अंबिया: 105)
यह शासन और साम्राज्य के बारे में इस्लामी शिक्षा की वास्तविक भावना है। इस बात को समझ लेने के बाद नबी (सल्ल.) के साथियों की विजयी कार्रवाइयों का औचित्य आसानी से समझा जा सकता है, जिससे उन्होंने सीज़र और कसरा के राज्य के सिंहासन को उखाड़ फेंका और असत्य के शासन के समस्त मायाजाल को नष्ट कर दिया।
अपने देश के सुधार के बाद जब उन्होंने बाहरी दुनिया को देखा, तो पाया कि सभी पड़ोसी देशों पर अत्याचारी राजाओं और सरदारों का बोलबाला है। ताक़त वालों ने कमज़ोरों को ग़ुलाम बना लिया है। अमीरों ने ग़रीबों को ख़रीद रखा है। मनुष्य, मनुष्य का देवता बना बैठा है। न्याय, और क़ानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजाओं और शासकों के इशारे पर लोगों के अधिकारों का हनन होता है, सम्मान लुटता है, घर नष्ट होते हैं और राष्ट्रों के भाग्य का फ़ैसला हो जाता है। ग़रीब मेहनतकश लोग अपना ख़ून पसीना एक कर जो धन कमाते हैं, उसे तरह-तरह के अत्याचारों के माध्यम से लूट लिया जाता है और अमीरों की विलासिता में उड़ा दिया जाता है। सत्ताधारी लोग स्वयं ही दुष्ट, अनैतिक और कामी हैं, इसलिए प्रजा भी हर प्रकार के पापों में लिप्त है। शराब, व्यभिचार और जुए की आम तौर पर अनुमति है, रिश्वतखोरी और विश्वासघात आम है। ईरान, रोम और मिस्र जैसे देश उस समय राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक आधारों पर जिस पतन का शिकार थे उनके उल्लेख से इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी हैं। दुष्कर्म में बाप-बेटी, और भाई-बहन तक का कोई भेद नहीं रह गया था। यहां तक कि धार्मिक नेता भी निकृष्टतम नैतिक अपराध में लिप्त थे। ईरान में मज्द के धर्म ने समाज की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। रोम में रईसों और सीज़रों की मनमानियां नैतिक पतन की चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं। मिस्र और अफ्रीका को रोमनों की ग़ुलामी ने पतन की गर्त में पहुंचा दिया था।
मानव समुदाय को इस अपमानजनक स्थिति में पीड़ित देखकर सुधारवादियों का वह साहसी समूह उनके सुधार के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले, उन्होंने धर्मोपदेशों और नसीहतों से काम लिया और इस्लाम के न्याय और धार्मिकता के क़ानून को अपनाने के लिए ईरान के ख़ुसरो, रोम के सीज़र और मिस्र के मुकोकस को आमंत्रित किया। जब उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तब उन्होंने मांग की कि शासन का पद उन लोगों के लिए ख़ाली किया जाए जो इसके पात्र हैं। लेकिन जब इस मांग को ठुकरा दिया गया और जवाब में तलवार दिखाई गई, तो मुट्ठी भर लोगों का यह साधनहीन समुदाय उठा और एक साथ दो महान साम्राज्यों को उखाड़ कर फेंक दिया, और भारत की सीमा से लेकर उत्तरी अफ्रीका तक, जो लोग उनके दमन और अत्याचार से रौंदे जा रहे थे, उन सब को एक ही बार में मुक्त कर दिया।
लोग चाहे इसे साम्राज्य विस्तार कहें, लेकिन इतिहास के इस कथन को नकारा नहीं जा सकता कि उनके शासन ने उन समुदायों को उस पतन से बाहर निकाला जिसमें वे गिरे हुए थे। उन्होंने उन्हें भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की ऊँचाई पर पहुँचाया और सभ्यता के लिए पूरी तरह से बंजर हो चुके देशों में वृद्धि और विकास की ऐसी शक्तियाँ पैदा कीं कि उनकी विरासत की महक आज तक मानव जगत में बनी हुई है। राष्ट्रवाद का धर्म तो शायद यही फ़ैसला करे कि ईरान और रोम चाहे नष्ट हो जाते, लेकिन अरबों को उन पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन सच्चाई का धर्म यह कहता है कि उन्होंने इस तरह से मानवता की सबसे बड़ी सेवा की है। वास्तव में यह दुनिया का दुर्भाग्य था कि उसका एक बड़ा हिस्सा उस समुदाय की सेवा से वंचित रह गया, जिस से ज़्यादा पवित्र समुदाय सूर्य की आंखों ने ज़मीन के चेहरे पर कभी नहीं देखी।
चौथा अध्याय
इस्लाम का प्रसार और तलवार
इस्लामी युद्ध के उद्देश्यों की इस व्याख्या में, जो पूरी तरह से क़ुरआन, पैग़म्बर (सल्ल.) की हदीसों और धर्म की प्रमाणिक किताबों पर आधारित थी, पाठकों ने देखा कि कहीं भी ग़ैर-मुस्लिमों को तलवार के बल पर इस्लाम में लाने का कोई आदेश नहीं है। किसी आदेश से यह अर्थ निकालना भी संभव नहीं है कि इस्लाम तलवार के बल पर लोगों को इस्लाम की सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। इस्लाम के युद्ध से जुड़े आदेशों में इस तरह के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति ही उस आरोप का खंडन करती है जो विरोधियों ने इसके ख़िलाफ़ लगाया है। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रस्त लेखकों और उनके जाहिल अनुयायियों ने इस मामले में दुनिया को जितना धोखा दिया है और ग़लतफ़हमियां फैलाई हैं, उन्हें देखते हुए यह ज़रूरी प्रतीत होता है कि इस विषय पर इस्लाम के सिद्धांतों और नियमों को पूरी स्पष्टता के साथ प्रसतुत कर दिया जाए।
पवित्र क़ुरआन की उन आयतों में जिनमें युद्ध के आदेशों की व्याख्या की गई है, युद्ध और रक्तपात के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ-साथ उसके लिए एक सीमा भी निर्धारित कर दी गई है और उससे आगे जाने की मनाही की गई है। यह सीमा एक या दो जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर बहुत स्पष्ट तरीक़े से खींची गई है। सूरह बक़रा में मुसलमानों को लड़ाई का आदेश देते हुए कहा गया है:
وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ (البقرہ: ۱۹۳)
“तुम उनसे लड़ते रहो, यहां तक कि उपद्रव शेष न रहे और धर्म केवल अल्लाह के लिए हो जाए।” (अल-बक़रा :193)
यहाँ एक मर्यादा बाँध दी गई है कि जब तक उपद्रव शेष रहे और धर्म के मार्ग में बाधाएँ हों तब तक युद्ध करना चाहिए और जब ये दोनों बातें दूर हो जाएँ तो युद्ध का द्वार बंद कर दिया जाए। तो आगे चल कर कहा:
لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ○ (البقرہ: ۱۹۳)
“अगर वे (उपद्रव करने से) रुक जाएं तो जान लो कि ज़ालिमों के सिवा किसी के लिए सज़ा नहीं है।” (अल-बक़रा :193)
सूरह मायदा में और भी स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि किस स्थिति में मानव जान अनुज्ञेय है और किस स्थिति में वर्जित:
أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۔ (المائدہ:۳۲)
“जो कोई दूसरे की जान ले बिना इस के कि उसने किसी की हत्या की हो, या ज़मीन में बिगाड़ पैदा किया हो, तो जैसे उसने सारी मानव जाति का ख़ून कर दिया।” (अल माइदाः 32)
इससे यह पता चला कि इंसान की हत्या केवल दो ही मामलों में की जा सकती है। एक यह कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति की अन्यायपूर्ण हत्या की और दूसरा यह कि उसने ज़मीन में फ़साद फैलाया। इन दोनों स्थितियों के अलावा किसी तीसरी स्थिति में उसकी हत्या करना न केवल अवैध है, बल्कि इतना बड़ा गुनाह है कि संसार का स्वामी उसे पूरी दुनिया की हत्या के बराबर मानता है।
सूरह अत-तौबा में युद्ध और लड़ाई की अंतिम सीमा जिज़्या अदा करने को ठहराया गया है, अत: कहा गया:
حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍۢ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ○ (التوبہ : ۲۹)
उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वे अपने हाथों से जिज़्या अदा न कर दें और आज्ञाकारिता स्वीकार न कर लें।” (अत-तौबा: 29)
इससे मालूम हुआ कि जब अवज्ञाकारी जिज़्या देकर इस्लामी नियम जारी करने को राज़ी हो जाएं तो उनसे लड़ाई नहीं की जा सकती और लड़ने की अनुमति की सीमा समाप्त हो जाती है।
सूरह शूरा में एक व्यापक सिद्धांत वर्णित किया गया है जो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता जो अल्लाह के बन्दों पर अत्याचार नहीं करते हैं और भूमि में अन्यायपूर्ण उपद्रव नहीं करते हैं:
وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ○ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ○ (الشوری: ۴۱ - ۴۲)
“और जो कोई अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, निंदा तो बस उनके लिए है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और ज़मीन में उपद्रव करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कष्टदायक यातना है।”(अश्शूरा :41-42)
सूरह अल-मुम्तहिना में स्पष्ट किया गया है कि मुसलमानों की दुश्मनी केवल उन अवज्ञाकारियों से है जो सत्य धर्म और सच्चे धर्म के अनुयायियों के दुश्मन हैं और जो ऐसे नहीं हैं, उनके साथ अच्छाई और भलाई का व्यवहार करने से मुसलमानों को कोई चीज़ नहीं रोकती:
لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ○ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ○ (المتحنه : ٩-٨)
“अल्लाह तुम्हें उन लोगों पर दया करने और न्याय करने से मना नहीं करता, जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में लड़ाई नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, क्योंकि अल्लाह न्याय करने वालों को मित्र रखता है। अल्लाह तो तुम्हें केवल उन लोगों से मित्रता करने से मना करता है, जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और शत्रुओं को तुम्हें निकालने में सहायता की। उन्हें जो मित्र बनाए वह विद्रोही है।” (अल-मुम्तहिना:8-9)
इन आदेशों का अर्थ इतना स्पष्ट है कि इसकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। उनसे स्पष्ट है कि इस्लामी युद्ध का वास्तविक उद्देश्य लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें अत्याचार, उपद्रव और विद्रोह से रोककर अल्लाह के क़ानून के अधीन लाना है।
इस्लाम की तलवार उन लोगों की गरदनें काटने के लिए तो बहुत तेज़ है, जो लोग इस्लाम और मुसलमानों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं या अल्लाह की भूमि में गड़बड़ी और बिगाड़ फैलाते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि ऐसा करने में वह सही नहीं है। लेकिन जो अत्याचारी नहीं हैं, जो दुष्ट नहीं हैं, जो अल्लाह की अवज्ञा नहीं करते हैं, जो सच्चे धर्म को मिटाने और दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो अल्लाह की सृष्टि की शांति और संतोष को भंग नहीं करते हैं, चाहे वे किसी भी राष्ट्र से संबंधित हों और उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी क्यों न हों, इस्लाम उनके जीवन और संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है। उसकी दृष्टि में उनका ख़ून हराम है।
धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं
युद्ध की सीमाओं का यह निर्धारण अपने आप में निर्नायक है, लेकिन अल्लाह की किताब की सुन्दरता यह है इस ने अलग से इसकी व्याख्या करके हमें यह भी बताया कि इस्लाम के प्रसार में ज़बरदस्ती और अनिच्छा की कोई भागीदारी नहीं है। सूरह बक़रा में स्पष्ट रूप से कहा गया है:
لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ○ (البقره: ۲۵۶)
“धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सीधे रास्ते को ग़लत रास्ते से अलग करके दिखाया जा चुका है, अब जो कोई भी झूठे देवताओं को त्याग देता है और अल्लाह पर विश्वास करता है, वह एक मज़बूत बंधन में शामिल हो जाता है जो टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह सुननेवाला और जानने वाला है।”(अल-बक़रा:256)
इस आदेश के शब्द बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन जिस मौक़े पर यह उतरा है, उसे सामने रखने पर यह और भी स्पष्ट हो जाता है। मदीना वालों का नियम था कि जब उनकी किसी महिला के बच्चे जीवित नहीं रहते, तो वह शपथ लेती कि अगर मेरा कोई बच्चा जीवित रहा, तो मैं उसे यहूदी बना दूंगी। मदीना में अंसार के कई बच्चों को इस विधि से यहूदी बनाया गया था। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बनी नज़ीर को उनकी हरकतों के लिए देश निकाला दिया, तो उनमें अंसार के बच्चे भी शामिल थे जो यहूदी धर्म के अनुयायी थे। अंसार ने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। हमने उन्हें उस समय यहूदी बनाया था जब हम उनके दीन को अपने से अच्छा समझते थे। लेकिन अब जब इस्लाम का सूर्य उदय हो गया है और हमारे पास सभी धर्मों से अच्छा धर्म है, तो हम अपने बच्चों को यहूदी नहीं रहने देंगे और उन्हें इस्लाम में आने के लिए मजबूर करेंगे। उस समय यह आदेश आया कि उन्हें मुसलमान बनने के लिए मजबूर न करो, क्योंकि धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
मुहम्मद इब्न इस्हाक़ ने हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से एक और हदीस बयान की है, जिसका अर्थ यह है कि अंसार के एक आदमी के दो बेटे थे जो ईसाई थे, वह अल्लाह के रसूल की सेवा में आया और कहा, “मेरे बेटे ईसाइयत छोड़ने के लिए सहमत नहीं हैं, क्या मैं उन्हें मजबूर कर सकता हूँ?” इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि दीन (धर्म) में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यह घटना हालांकि पिछली घटना से अलग है, लेकिन दोनों का मक़सद समान है।
क़ुरआन के जाने-माने व्याख्याकार अल्लामा ज़मख़शरी ने भी इस आयत की व्याख्या करते हुए “कश्शाफ़” में लिखा हैं:
“अल्लाह ने ईमान के मामले में बलप्रयोग और ज़बरदस्ती को हस्तक्षेप नहीं दिया है, बल्कि इसे सामने वाले की इच्छा और अधिकार पर छोड़ दिया है। अगर अल्लाह की इच्छा लोगों को मुसलमान बनाने की होती, तो वह लोगों को ईमान करने के लिए मजबूर कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सारा मामला लोगों के विवेक पर ही रखा।”
इमाम राज़ी, अपनी व्याख्या में इस आयत के बारे में लिखते हैं:
सर्वशक्तिमान अल्लाह ने इस आयत के बाद ही कह दिया है, मार्गदर्शन को पथभ्रष्टता से अलग और स्पष्ट करके दिखाया जा चुका है, अर्थात तर्क और प्रमाण खोल-खोल कर बताए जा चुके हैं अब इसके बाद केवल मजबूर करने और ज़बरदस्ती करने का रास्ता बचता है जो जायज़ नहीं है, और जिसकी अनुमति नहीं है क्योंकि यह दायित्व के विपरीत है।
अगर इस्लाम की शिक्षा यह होती कि लोगों को तलवार के बल पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो इस्लामी राष्ट्र बीती 14 शताब्दियों में कम से कम एक बार तो इस शिक्षा के अनुसार लोगों को इस्लाम में लाने के लिए मजबूर करते। इतना ही नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि सच्चे ख़लीफ़ाओं के उज्ज्वल काल के दौरान भी, जब इस्लाम अपनी वास्तविक महिमा में चमक रहा था, और ख़ुद पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) के पवित्र शासन के दौरान भी, जो क़ुरआन की व्यावहारिक व्याख्या था, कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया गया। पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) को बार-बार अवज्ञाकारियों पर अधिपत्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम का फंदा उनकी गर्दनों में कभी नहीं डाला, बल्कि अपनी शुद्ध शिक्षा से उनके दिलों के मैल दूर करने पर ही संतोष किया। जिन लोगों को आप इस्लाम की दावत के लिए भेजते, उनसे आग्रह करते कि वे लोगों पर कठोरता न करें।
अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा तो कहा, “नर्मी करना, सख़्ती न करना, ख़ुश करना, नफ़रत न दिलाना।” जब आपका मक्का में विजयी प्रवेश हुआ, तो आपने उन अवज्ञाकारियों को, जो आपके ख़ून के प्यासे थे, यह कह कर कि “आज तुम पर कोई आरोप नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो”, आज़ाद छोड़ दिया और किसी को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। (उन आज़ाद छोड़े हुए लोगों में से दो हज़ार लोगों ने अपनी मर्ज़ी से हुनैन की लड़ाई में उनका साथ दिया)
मक्का के उपनगरों में, उन्होंने जो समूह इस्लाम के प्रसार के लिए भेजे उन्हें लड़ने से मना किया। जब हज़रत ख़ालिद ने अल्लाह के रसूल की अनुमति के विरुद्ध बनी जज़ीमा जनजाति में रक्तपात किया, तो नबी (सल्ल.) ने सार्वजनिक रूप से उसे इस्लाम विरोधी बताया और उस जनजाति के कुत्तों तक के ख़ून का हर्जाना चुकाया। ये तो कुछ मिसालें हैं, वरना पैग़म्बर मुहम्मद (स.अ.व.) की पूरी जिंदगी में एक भी ऐसी घटना नहीं मिलती कि उन्होंने किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर इस्लाम कुबूल करने पर मजबूर किया हो।
इस्लाम के आह्वाण और उपदेश का मूल सिद्धांत
तथ्य यह है कि युद्ध के आदेश की आयत या जिज़्या की आयत का विषय “दीन (धर्म) में कोई ज़बरदस्ती नहीं है” की धार्मिक स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों ने ग़लती से समझ लिया है, बल्कि यह केवल उस स्वतंत्रता को, जो आरंभ में बिना शर्त दी गई थी, एक नियम और एक सिद्धांत के अधीन ले आता है। आरंभ में, जब मुसलमान कमज़ोर थे और उनमें वह काम करने की ताक़त नहीं थी जो अल्लाह उनसे एक मध्य समुदाय के रूप में लेना चाहता था, तो मुसलमानों को यह कहने की शिक्षा दी गई थी, “तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन”, और “हमारे कर्म हमारे साथ और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ।” उनके पास इतनी ताक़त नहीं थी कि वे दुनिया को बलपूर्वक नैतिक बिगाड़ से मुक्त कर सकें और फ़ितना और बिगाड़ को समूल मिटा सकें। इसीलिए भलाई का आदेश और बुराई का निषेध दोनों एक ही तरह से किए जाते रहे। दूसरे शब्दों में, जिस तरह अल्लाह के रसूल अपने मानने वालों को एकेश्वरवाद क़ुबूल करने, नुबूवत क़ुबूल करने, आखिरी दिन पर ईमान लाने और नमाज़ क़ायम करने के लिए कहते थे, उसी तरह व्यभिचार, चोरी, बच्चों की हत्या, झूठ, आदि से घृणा भी दिलाते थे और केवल बोलकर बुराइयों से रोकते थे। लेकिन जब मुसलमान कमज़ोरी और लाचारी की स्थिति से बाहर निकले और उन्हें अपने मिशन को व्यवहारिक रूप देने की शक्ति मिल गई, तो धार्मिक स्वतंत्रता का यह सिद्धांत तो अपनी जगह बना रहा कि किसी भी व्यक्ति को जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यह तय किया गया कि जहां कहीं भी हमारे वश में होगा, लोगों को दुष्कर्म, उपद्रव और दूसरे बुरे कामों की आज़ादी नहीं दी जाएगी। तो, उस समय, “अम्र बिल-मारूफ़” का दायरा “नह्यी अनिल-मुनकर” से अलग हो गया। “नह्यी अनिल-मुनकर” में, तो उपदेश के साथ तलवार भी जुड़ गई, और उसने पूरी दुनिया को फ़ितना और बिगाड़ से मुक्त करने का बीड़ा उठा लिया, चाहे दुनिया उसपर सहमत हो या न हो, लेकिन “अम्र बिल-मारूफ़” के दायरे में, वही “दीन (धर्म) में कोई ज़बरदस्ती नहीं है” का सिद्धांत बरक़रार रहा।
हम पहले कह चुके हैं कि इस्लाम के दो स्वरूप हैं। एक रूप में, यह संसार के लिए अल्लाह का नियम है। दूसरे रूप में, यह अच्छाई और पवित्रता का आह्वान है। पहले रूप का उद्देश्य दुनिया में शांति स्थापित करना और इसे दुष्ट और विद्रोही लोगों द्वारा नष्ट होने से बचाना और दुनिया के लोगों को नैतिकता और मानवता की सीमाओं का पालनकर्ता बनाना है, जिसके लिए बल प्रयोग ज़रूरी है। दूसरे रूप में, वह दिलों को शुद्ध करने वाला, आत्माओं को शुद्ध करने वाला, और अशुद्धियों को दूर करके मनुष्यों को श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाने वाला है, जिसके लिए तलवार की धार नहीं, बल्कि मार्गदर्शन का प्रकाश आवश्यक है।
अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर तलवार चमकती देखकर “ला इलाहा इल्लल्लाह” कह दे, मगर उसका दिल अल्लाह के सिवा दूसरे बुतों से भरा हो, तो दिल की पुष्टि के बिना ज़बान की यह स्वीकारोक्ति किसी काम की नहीं है। सत्य धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, संसार के छोटे-छोटे आंदोलन भी, जिनका उद्देश्य सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, अपनी सफलता के लिए ऐसे अनुयायियों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, जो केवल मुंह से सहानुभूति रखते हों, लेकिन दिल से साथ न हों। झूठे अनुयायियों को लेकर आजतक किसी आंदोलन ने सफलता का मुंह नहीं देखा है। फिर अच्छी तरह से विचार करें कि जिस धर्म की दृष्टि केवल इहलोक की सफलता पर नहीं परलोक की सफलता पर हो, जो धर्म नीयत और विश्वास को कर्म का आधार मानता हो, जो धर्म संपूर्ण हृदय की पवित्रता और सच्चाई के बिना किसी काम का कोई मूल्य न समझता हो, क्या यह संभव था कि उसने अपने प्रसार का काम तलवार को सौंप देता? क्या ऐसा हो सकता था कि वह ईमानदारी और सच्चाई को छोड़कर जबरन आज्ञाकारिता और मजबूरी की स्वीकारोक्ति पर संतुष्ट हो जाता? क्या वह ऐसे अनुयायियों से संतुष्ट हो सकता है जिनके हृदय अल्लाह के भय से ख़ाली हैं लेकिन तलवार के भय से भरे हुए हैं? क्या वह ऐसे कायर पुरुषों को कोई विज़न दे सकता था, जो केवल अपनी जान बचाने के लिए, एक ऐसी आस्था को स्वीकार कर लें, जिसकी सच्चाई का उन्हें यक़ीन न हो? अगर वह ऐसा होता, तो क्या वह उस सफलता को हासिल कर सकता था जो उसने वास्तव में हासिल की?
मनुष्य के स्वभाव को उसके निर्माता से बेहतर कौन समझ सकता है? उसने इस विषय को अपने तत्वदर्शी ग्रंथ में बहुत ही शानदार तरीक़े से समझाने की कोशिश की है और अपने रसूल को भी विधिपूर्वक बताया है कि दिलों को जीतने का सही और प्रभावी तरीक़ा क्या है। अतः एक स्थान पर कहा गया हैः
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ○(حٰمٓ السجدہ :۳۴)
“ऐ पैग़म्बर भलाई और बुराई समान नहीं होते, तो बुराई को उस तरीक़े से दूर करो, जो सर्वोत्तम हो। फिर देखो कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी है वह तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा।” (हा-मीम सजदा :34)
दूसरे स्थान पर कहा गया:
فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۔ۖ (آل عمران : ۱۵۹)
“यह अल्लाह की मेहरबानी है कि तू उनके लिए नर्मदिल बनाया गया है, नहीं तो अगर तू कड़क और सख़्तदिल होता तो ये तुझे छोड़कर अलग हो जाते।” (आले-इमरान: 159)
एक अन्य स्थान पर इस्लाम की ओर बुलाने का तरीक़ा यह बताया कि:
ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ۔ (النحل: ۲۵)
“उन्हें अपने रब के रास्ते की ओर तत्वदर्शिता और अच्छे उपदेश और नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बेहतरीन तरीक़े से बहस करो।” (अल-नहल: 125)
नर्मी और शब्दों की मिठास पर इतना ज़ोर दिया कि अवज्ञाकारियों के देवताओं और धर्मगुरुओं की बुराई करने से भी रोक दिया गया:
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ۔ (الانعام:۱۰۸)
“उनके मिथ्या देवताओं की निन्दा न करना जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, नहीं तो वे अज्ञानता के कारण अल्लाह की निन्दा करेंगे।” (अल-अनआम: 108)
मार्गदर्शन और गुमराही का रहस्य
फिर विभिन्न अवसरों पर इस सूक्ष्म बिन्दु को समझाया गया है कि अगर अल्लाह चाहे तो अपने बन्दों को ईमान लाने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन उसे ऐसे जबरन ईमान की ज़रूरत नहीं है जो शारीरिक इच्छाओं और भावनाओं की तरह मनुष्य की प्रवृत्तियों में समाया हुआ हो। ऐसा ईमान रखने वाला और आज्ञाकारी करने वाला प्राणी पहले से ही उसके पास मौजूद था, जिसका स्वभाव ही यह है कि वे वही करते हैं، जिनका उन्हें आदेश दिया जाता है। लेकिन अल्लाह को एक ऐसा प्राणी चाहिए था, जिसे उसकी आज्ञा मानने के लिए कोई ताक़त मजबूर न करे, बल्कि वह ख़ुद अपनी बुद्धि से, अपनी खोज से उसे पहचाने और अपनी मर्ज़ी से उसकी पूजा करे। उसकी आज्ञाओं को न मानने की शक्ति होने के बावजूद उसका पालन करे। इसी उद्देश्य के लिए अल्लाह ने मनुष्य को बनाया। उसने उसे एक निश्चित अवधि के लिए, बुद्धि के प्रकाश में मुक्त छोड़ दिया कि 'जो चाहे ईमान लाए और जो छाहे अवज्ञा करे। उसकी ओर एक के बाद एक पथप्रदर्शक भेजे, ताकि उसे मार्गदर्शन और पथभ्रष्टता अलग-अलग करके दिखा दी जाए और उसके लिए यह बहाना बनाने की कोई जगह न रहे कि हम पूर्ण अंधकार में थे। फिर उसके लिए एक हिसाब का दिन निर्धारित किया ताकि जिन लोगों ने अपनी बुद्धि से उसे पहचाना है और अपनी मर्ज़ी से उसके द्वारा निर्देशित सीधे रास्ते को अपनाया उन्हें वह उस दिन अंतहीन इनाम दे। और जिन लोगों ने स्पष्ट संकेतों के बावजूद गुमराही अपनायी, उसके द्वारा भेजे गए संदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया, उन्हें दर्दनाक सज़ा दे।
देखें कि कैसे इस रहस्य को प्रकट किया है:
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١١٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ○ (هود: ۱۱۸-۱۱۹)
“अगर तेरा रब चाहता तो वह सभी लोगों को एक ही समुदाय बना देता, मगर वे मतभेद करते रहेंगे, सिवाय उन लोगों के कि जिन पर अल्लाह ने दया की है और इसी के लिए उसने उन्हें पैदा किया है। इस प्रकार तुम्हारे रब की वह बात पूरी हौ गई जो उसने कही थी कि मैं नरक को जिन्नों और मनुष्यों से भर दूँगा।” (हूद: 118-119)
अन्य स्थानों पर भी यह रहस्य भिन्न-भिन्न प्रकार से उद्घाटित हुआ है, इसलिए कहीं कहा गया है:
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ○ (یونس :۹۹)
“और अगर तुम्हारा रब चाहता तो धरती पर बसने वाले सब के सब ईमान ले आते।” (यूनुस: 99)
कहीं कहा:
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ (الانعام :۱۰۷)
“और अगर अल्लाह चाहता तो वे कभी शिर्क न करते (उसका साझी न ठहराते)।” (अनआम:107)।
कहीं कहा:
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةًۭ فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ○ (الشعرا: ۴)
“अगर हम चाहते तो उन पर आसमान से ऐसी निशानी उतारते, जिसे देख कर वे सजदा करने पर मजबूर हो जाते।” (अश्शुअरा: 4)
कहीं कहा:
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○ (یونس:۱۰۰)
“अल्लाह की अनुमति के बिना कोई भी ईमान नहीं ला सकता, और अल्लाह का तरीक़ा यह है कि जो लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते उन पर गंदगी डाल देता है।” (यूनुस: 100)
उसने कहीं कहा:
إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ○ (القصص :۵۶)
“वास्तव में, आप जिसे चाहते हैं, उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है, उसका मार्गदर्शन करता है और वह जानता है कि कौन मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए तैयार है।” (अल-कसस: 56)
तो जब सर्वशक्तिमान और सृष्टिकर्ता प्रभु ख़ुद अपने बन्दों को अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करना नहीं चाहता, बल्कि वह उनकी स्वतंत्रता को अधिक प्रिय रखता है, तो फिर एक बन्दे को यह अधिकार कैसे मिल सकता है कि अपने जैसे बन्दों को उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करे। यही वजह है कि अल्लाह ने इस्लाम के आवाहक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को बार-बार समझाया है कि धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और तुम्हारे लिए बस ख़ुदा का पैगाम पहुंचा देना ही काफ़ी है:
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍۢ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ○ (ق :۴۵)
“तू उन्हें मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए बाध्य करने वाला नहीं है, जो कोई अल्लाह की धमकी से डरने वाला हो, उसे क़ुरआन से नसीहत किए जा।” (क़ाफ़:45)
فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌۭ ○ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ○(الغاشیہ :۲۱-۲۲)
“तू नसीहत किए जी, क्योंकि तू केवल नसीहत करने वाला है, तू उन पर कोई दारोग़ा नहीं है।” (अल-ग़शियह: 21-22)
أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ○ (یونس :۹۹)
“क्या आप लोगों को ईमान लाने के लिए मजबूर करेंगे? (हालांकि आपका काम मजबूर करना नहीं है)।” (यूनुस: 99)
لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ○ (البقرۃ:۲۷۲)
“उनका मार्गदर्शन तुम्हारा दायित्व नहीं है, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मार्गदर्शन करता है।” (अल-बकरा: 272)
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ○ (الرعد:۴۰)
“संदेश पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है और हिसाब लेने के लिए हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं।” (अल-राद: 40)
इस्लाम के प्रसार में तलवार की भूमिका
इस चर्चा से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि इस्लाम किसी को भी अपनी प्रामाणिकता पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह तर्कों और प्रमाणों के आलोक में मार्गदर्शन और पथभ्रष्टता का मार्ग दिखा देने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को यह विकल्प देता है कि वह चाहे ग़लत रास्ते पर चलकर असफलता के गर्त में जा गिरे और चाहे तो सीधे रास्ते पर चलकर सच्ची और स्थायी सफलता का आनंद ले। लेकिन इस शृंखला को समाप्त करने से पहले हम इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि इस्लाम के प्रसार का संबंध कुछ न कुछ तलवार से ज़रूर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ तक ईश्वरीय धर्म के प्रचार का संबंध है, उसमें तलवार का कोई काम नहीं है। लेकिन इस उपदेश के साथ-साथ अन्य चीज़ें भी हैं जो दुनिया में इस्लाम के प्रसार में योगदान करती हैं, और वे निश्चित रूप से तलवार से अंजान नहीं हैं।
आम तौर पर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वतंत्रता का जीवन जीता है और अपनी इच्छाओं के पालन में किसी नैतिक संहिता से बंधा नहीं होता है, तो उसे अपने दर्दनाक लेकिन सुखद प्रतीत होने वाले जीवन में एक आनंद आने लगता है और वह इस मज़ा को छोड़ देने के लिए अहनी मर्ज़ी से तैयार नहीं होता। उपदेशों, तर्कों और प्रमाणों के बल पर उसे नैतिक मर्यादाओं का पालन करने, हलाल और हराम के बीच अंतर करने और अच्छे और बुरे के बीच भेद करने की कितनी ही प्रेरणा दी जाए, वह किसी तरह सीधा होने पर सहमत नहीं होता। पहली बात तो यह निरन्तर बुरे कर्म करने के कारण उसकी बुद्धि और विवेक पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि इस प्रकार की नैतिक शिक्षा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अगर उसके अन्तःकरण में कुछ जीवन शेष भी है तो वह इतना प्रबल नहीं होता कि उसके प्रभाव से वह सत्य को स्वीकार कर ले, और उन सुखों का त्याग कर दे जो स्वतंत्रता के जीवन में उसे प्राप्त हैं। दूसरी ओर जब किसी नैतिक शिक्षा के पीछे उपदेश और नसीहत के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति और दंड का प्रावधान भी होता है और बुराई को रोक देने की शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, तो धीरे-धीरे स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है। मर्यादाओं का पालन और अच्छे और बुरे के बीच का भेद धीरे-धीरे विकसित होने लगता है और अंत में वही व्यक्ति अच्छाई की शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करने लगता है जिसे वह अपने स्वच्छंद जीवन में सुन भी नहीं सकता था।
थोड़ी देर के लिए एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जिसमें कोई क़ानून लागू नहीं है, हर कोई नैतिक सीमाओं से मुक्त है, जिस पर बस चलता है उसे लूटता है, जिस किसी से भी नफरत करता है उसे मार डालता है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे चोरी करके या छीन कर प्राप्त कर लेता है। जो इच्छा पैदा होती है उसे जैसे चाहता है पूरा कर लेता है। वह सही और ग़लत में भेद नहीं करता। उसके सामने केवल उसकी इच्छाएँ होती हैं और उन्हें पूरा करने के संभावित साधन। ऐसी स्थिति में, अगर कोई नैतिक सुधारक खड़ा हो और लोगों को हलाल और हराम के बीच अंतर करना सिखाए, जायज़ और नाजायज़ का भेद समझाए, अच्छे और बुरे तरीक़ों के बीच अंतर स्थापित करे, चोरी और हराम के सेवन से उन लोगों को रोके, अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करे, और एक पूर्ण आचार संहिता बना डाले, लेकिन इस क़ानून के कार्यान्वयन के लिए उसके पास कोई शक्ति न हो, तो क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वह समाज अपनी स्वतंत्रता पर इन प्रतिबंधों को सहर्ष स्वीकार कर लेगा? कोई भी व्यक्ति जो मानव स्वभाव के रहस्य से परिचित हो, इस प्रश्न का उत्तर केवल नकारात्मक ही देगा। क्योंकि संसार में ऐसी शुद्ध आत्माओं की संख्या बहुत कम है जो अच्छाई को केवल अच्छाई समझकर अपना लेते हैं और बुराई को केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बुरा होना उन्होंने जान लिया है।
लेकिन अगर यही सवाल इस स्थिति में किया जाए कि वह नैतिक उपदेशक एक शक्तिशाली शासक और नेता भी हो और देश में एक औपचारिक सरकार की स्थापना करदे, जिसकी शक्ति से उन सभी बुराइयों का अंत हो जाए, तो निश्चित रूप से यह जवाब सकारात्मक हो जाएगा और सभी इस कल्याणकारी शिक्षा की सफलता की घोषणा करेंगे।
इस्लाम के प्रसार का भी लगभग यही हाल है। अगर इस्लाम केवल कुछ मान्यताओं का संग्रह होता और अल्लाह को एक मानने, पैग़म्बर (सल्ल.) को ईशदूत मानने, अंतिम दिन और स्वर्गदूतों पर विश्वास करने के अलावा किसी और चीज़ की मांग नहीं करता, तो शायद शैतानी शक्तियों के साथ ज़्यादा झगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तथ्य यह है कि इस्लाम केवल एक आस्था ही नहीं बल्कि एक क़ानून भी है, एक ऐसा क़ानून जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को आज्ञाओं और निषेधों के बंधनों में कसना चाहता है, इसलिए उसका काम केवल उपदेश से नहीं चल सकता, बल्कि इसे ज़ुबान के साथ-साथ तलवार से भी काम लेना पड़ता है। कोई व्यक्ति इसकी आस्थाओं के प्रति उतना विद्रोही नहीं है जितना कि इसके क़ानूनों का पालन करने से इंकारी है। वह चोरी करना चाहता है और इस्लाम उसे हाथ काट देने की धमकी देता है, वह व्यभिचार करना चाहता है और इस्लाम उसे कोड़े मारने का आदेश देता है, वह सूद लेना चाहता है और इस्लाम उसे अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ लड़ाई की चुनौती देता है। वह वर्जित और वैध के बंधन से मुक्त होकर मनेच्छाओं को पूरा करना चाहता है और इस्लाम उसे इस की इजाज़त नहीं देता। यही कारण है कि मनेच्छाओं का पालन करने वाले व्यक्ति का स्वभाव इससे घृणा करता है और उसके दिल का आईना गुनाहों के दाग़ से ऐसा भर जाता है कि उसमें इस्लाम की सच्चाई के प्रकाश को स्वीकार करने की क्षमता नहीं बचती है।
यही कारण है कि पैग़म्बर (सल्ल.) 13 वर्षों तक अरबों को इस्लाम की शिक्षा देते रहे, उन्होंने उपदेश और प्रेरणा का सबसे प्रभावी और कुशल तरीक़ा अपनाया, उन्होंने मज़बूत तर्क और प्रमाण दिए, अपनी नैतिकता और अपने शुद्ध जीवन से सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया और सच्चाई को व्यक्त करने और उसकी पुष्टि करने का कोई भी साधन नहीं छोड़ा, लेकिन मक्कावासियों ने उनके निमंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सच्चाई उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी। उन्होंने देख लिया था कि जिस रास्ते की ओर उनका पथप्रदर्शक उन्हें बुला रहा था, वह सीधा रास्ता है, फिर भी केवल यह बात उन्हें सच्चाई का रास्ता अपनाने से रोक रही थी, कि वे उन सुखों को त्यागने को तैयार न थे, जिनका वे अपने स्वच्छंद जीवन में आनंद उठा रहे थे। लेकिन जब धर्मोपदेशों की असफलता के बाद इस्लाम के पैग़म्बर ने हाथ में तलवार लेकर सभी वंशानुगत भेदभावों को समाप्त कर दिया, सभी झुठी औपचारिकताओं को तोड़ दिया और एक व्यवस्थित और अनुशासित सरकार की स्थापना कर दी, नैतिक क़ानूनों को लागू करके, गुनाह करने की स्वतंत्रता छीन ली, और शांति का वातावरण बना दिया जो नैतिक गुणों के विकास के लिए हमेशा आवश्यक होता है, तो धीरे-धीरे दिलों से बुराई और दुष्टता का धब्बा छूटने लगा, प्रकृति से बिगाड के अवयव आप से आप दूर हो गए, इतना ही नहीं, आंखों से पर्दे हट गये और सत्य का प्रकाश स्पष्ट हो गया।
अरबों की तरह अन्य देशों ने भी जो इस्लाम को इतनी तेज़ी से स्वीकार किया कि एक सदी में ही एक चौथाई दुनिया मुसलमान हो गई, तो उसका कारण भी यही था कि इस्लाम की तलवार ने उनके दिलों पर पड़े पर्दों को फाड़ दिया। उस वातावरण को साफ़ कर दिया जिसमें कोई नैतिकता पनप नहीं सकती थी। उन साम्राज्यों को उखाड़ फेंका जो सत्य के दुश्मन और असत्य के संरक्षक थे। उन बुराइयों का उन्मूलन कर दिया जो दिलों को अच्छाई और ईशपरायणता से दूर रखती हैं। फिर इस्लाम को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि मनुष्य के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इससे बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता। इसलिए जैसे यह कहना ग़लत है कि इस्लाम तलवार के बल पर लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करता है, वैसे ही यह कहना भी ग़लत है कि तलवार का इस्लाम के प्रसार में कोई हिस्सा नहीं है। सच्चाई इन दोनों के बीच है, और वह यह है कि इस्लाम के प्रसार में उपदेश और तलवार दोनों की भूमिका है, जैसा कि हर सभ्यता की स्थापना में होता है।
दुनिया के पूरे इतिहास में हमें ऐसी किसी भी सभ्यता का पता नहीं चलता है, जिसकी स्थापना में इन दोनों तत्वों की हिस्सेदारी न हो। सभ्यता के किसी विशेष रूप का क्या उल्लेख, सभ्यता की स्थापना तब तक असंभव है जब तक कि ज़मीन तैयार करने और बीज डालने की ये दोनों प्रक्रियाएँ अपनी भूमिका नहीं निभाएं। मानव स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि समुदायों के मानसिक और नैतिक सुधार की प्रक्रिया में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हृदय और आत्मा को संबोधित करने से पहले शरीर और जान को संबोधित करना पड़ता है।
पांचवां अध्याय
शांति और युद्ध के इस्लामी क़ानून
पिछले अध्यायों में जो वर्णित किया गया है वह केवल युद्ध के नैतिक पक्ष से संबंधित था। अब हम बताना चाहते हैं कि युद्ध के व्यवहारिक पहलू में इस्लाम ने कितना बड़ा सुधार किया है।
किसी काम का अच्छा और बुरा होना दो बातों के आधार पर तय होता है। एक लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीक़ा। अगर लक्ष्य अपने आप में अच्छा नहीं है, तो इसे प्राप्त करने के साधन चाहे कितने ही महान क्यों न हों, लक्ष्य को श्रेष्ठता प्रदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य अनाथों का पालन पोषण और उनको शिक्षित करना और विधवाओं को सहारा देना है, लेकिन इस अच्छे काम के लिए वह चोरी और लूट के माध्यम से रुपये कमाता है, तो इसके बावजूद कि उसका लक्ष्य बहुत पवित्र है, क़ानून और नैतिकता की दृष्टि से उसके तरीक़े अर्थात् चोरी को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उसे चोर ही समझा जाएगा। इसके विपरीत एक अन्य व्यक्ति वास्तव में लोगों को धोखा देकर रुपये कमाना चाहता है, लेकिन वह लोगों पर अपना विश्वास स्थापित करने के लिए मस्जिद में बैठकर धार्मिक ज्ञान बांटता है, भलाई के उपदेश देने में अपना सारा समय व्यतीत करता है। अतएव यद्यपि उसके ये कर्म बड़े ही पवित्र होते हैं, परन्तु वह जिस मलिन प्रयोजन का ढोंग करता है, वह न केवल उसके सत्कर्म रूपी धन का नाश करता है, अपितु मिथ्या धर्मपरायणता द्वारा उसके अपराध को और भी गंभीर बना देता है।
युद्ध का भी यही हाल है। अगर युद्ध का उद्देश्य कमज़ोर राष्ट्रों की स्वतंत्रता को छीनना, देशों की संपत्ति को लूटना और अल्लाह के बन्दों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना है, तो इस तरह के युद्ध को चाहे कितने ही संयम और अनुशासन के साथ लड़ा जाए, उसमें ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े न अपनाए जाएं, घायलों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, संधियों का कितना भी सम्मान किया जाए, चाहे वह लूटपाट, आगज़नी, नरसंहार और आमजनों के अपमान से कितना ही दूर क्यों न हो, यह युद्ध अनिवार्य रूप से दमन और अत्याचार ही कहलाएगा। इस अनुशासन और प्रबंधन से उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आएगा। अधिक से अधिक, उसे क्रूरता का एक सभ्य रूप कहा जा सकता है। इसी तरह, अगर युद्ध का उद्देश्य बहुत ही नेक है, उदाहरण के लिए, यह एक वैध हित की रक्षा के लिए या बिगाड़ को दूर करने और बुराई को दूर करने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन इसके तरीक़े क्रूर हैं, कोई नैतिक सीमा नहीं है, इसमें लड़ाके दुश्मन का सफ़ाया करना चाहते हैं, उसे तड़पा-तड़पा कर बदले की आग बुझाना चाहते हैं तो ऐसे युद्ध को भी सत्य के रास्ते से भटका हुआ माना जाएगा। युद्ध का उद्देश्य सही होने के बावजूद इसके लड़ाकों को क्रूर और अत्याचारी ही कहा जाएगा।
इसलिए वैध और पवित्र धर्मयुद्ध की परिभाषा यह है कि उसका लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के साधन दोनों ही पवित्र और नेक हों। युद्ध की इस्लामी शिक्षा के बारे में अब तक जो कुछ कहा गया है, वह केवल उसके कारण की पवित्रता और श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। अभी चर्चा का दूसरा पक्ष शेष है, इसलिए इस अध्याय में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि लक्ष्य प्राप्त करने की विधि के संदर्भ में इस्लाम का युद्ध सभ्यता और कुलीनता के इस मानक को कहाँ तक पूरा करता है।
यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि इस्लाम की युद्ध पद्धति का विवरण देने से पूर्व हम यह भी देख लें कि प्राचीन काल में युद्ध के प्रति ग़ैर-मुस्लिम राष्ट्रों और समुदायों का दृष्टिकोण क्या था। इससे हम इस सुधार के मूल्य का अधिक सटीक आकलन कर सकेंगे जो इस्लाम ने इस मामले में किया है।
(1) युद्ध के पूर्व-इस्लामी, अरब तरीक़े
अरब समुदायों में, युद्ध बहुत आम था। आजीविका के साधनों की कमी, और सामूहिक अनुशासन और व्यवस्था के अभाव के कारण, अरबों में युद्ध की ऐसी आदत स्थापित हो गई थी कि वे हत्या, रक्तपात और लूटपाट को अपनी विशेषता, बल्कि अपना गौरव मानने लगे थे। सम्भवतः आरम्भ में इसकी ज़रूरत केवल पेट भरने, जलस्रोत में हिस्सेदारी पाने, चरागाहों में पशु चराने या बदला लेने के लिए पड़ती होगी। लेकिन सदियों से तलवारबाज़ी और नरसंहार के खेल में लगे रहने के कारण वे इतने रक्तपिपासु हो गए थे कि रक्तपात के लिए उन्हें किसी उद्देश्य की ज़रूरत नहीं रह गई थी, बल्कि रक्तपात ही उनका उद्देश्य बन गया था। इसके साथ ही क्रूरता, हृदयहीनता, बदले की भावना, द्वेष, उग्रता, हिंसा आदि वे सभी लक्षण जो इस तरह का जीवन जीने से स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, उनके चरित्र के प्रमुख अवयव हो गए थे। कुलों और परिवारों में दुश्मनियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगी थीं। उग्र प्रतिशोध की आग को बुझाने और शत्रुकुल का सर्वनाश करने के लिए, बर्बर से बर्बर तरीक़े अपनाए जाते थे। गौरव और बहादुरी की अभिव्यक्ति के लिए अकारण ख़ून बहाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता था।
युद्ध की अरबी अवधारणा
प्राचीन अरब के हालात का पता लगाने के लिए हमारे पास केवल दो स्रोत हैं। एक वे (दास्तानें) कहानियां, जो अय्यामुल अरब के नाम से अरबों के बीच लोकप्रिय थीं। दूसरे अरब कवियों के काव्य जिनमें वे अपनी संस्कृति और समाज के मामलों और भावनाओं का सटीक चित्रण करते थे। शेष दुनिया की भाँति उनका काव्य सूक्ष्म कल्पनाओं और अतिशयोक्तियों का संग्रह नहीं था, अपितु वे अपने चारों ओर जो देखते थे, उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते थे। अतः उनका काव्य केवल काव्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का चित्रण भी था। युद्ध के बारे में अरबों की क्या धारणा थी? उनके लड़ने के तरीक़े क्या थे? दुश्मन के साथ उनका व्यवहार कैसा था? वे कौन सी प्रेरणाएँ थीं, जो उन्हें लड़ने पर उभारती थीं? वे किन लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए लड़ते थे? इन सभी सवालों का जवाब हमें उन कविताओं में मिलता है। युद्ध पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन शब्दों, उपमाओं और रूपकों का इस्तेमाल किया है, वे युद्ध के उनके प्रारूप का एक सटीक चित्रण करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ हम कुछ शब्दों और भावों और रूपकों और उपमाओं को उद्धृत करते हैं:
हर्ब - युद्ध के लिए एक सामान्य शब्द है। शब्दकोश में इसका वास्तविक अर्थ ग़ुस्सा करना है।
तहरीब - का मतलब ग़ुस्सा दिलाना, उकसाना और भाले को तेज करना है।
हरब - किसी की संपत्ति लूट लेना।
हरबिया - लूटा हुआ माल जिस पर व्यक्ति के जीवन का साधन होता है।
महरूब और हरीब - वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति लूट ली गई है।
अहराब - शत्रु की संपत्ति को लूटने के लिए किसी का नेतृत्व करना।
रौअ - आमतौर पर लड़ाई के लिए बोला जाता है। इसका मूल अर्थ डर और भय है।
अर्थात् युद्ध को एक भयानक चीज़ कहा गया है। विदाक बिन तमसील अल-माज़नी कहता है:
“वे आगे बढ़ने वाले और युद्ध के खतरे में क़दम मिलाकर चलने वाले हैं।”
वग़ी - यह भी लड़ाई का एक जानामाना नाम था। इसका शाब्दिक अर्थ शोर और हंगामा है। कवि कहता है:
“बनू मुर्रा की विशेषता हमेशा से ज्ञात रही है, कि वे युद्ध में अपने दुश्मनों के ख़ून से बार-बार अपने भालों की प्यास बुझाते हैं, और कम से कम एक बार उनकी प्यास बुझाना तो उनपर अनिवार्य है।”
शर - शाब्दिक अर्थ है बुराई और युद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कवि अपनी जनजाति की प्रशंसा इस प्रकार करता है:
“वे ऐसे लोग हैं कि जब लड़ाई उन्हें डराती है तो वे समूह बना-बना कर और अकेले-अकेले उसका सामना करने दौड़ पड़ते हैं।”
करीहा - यह भी युद्ध के नामों में से एक है और इसका मूल अर्थ कठिनाई, परेशानी और विपत्ति है। कवि अपने लोगों की प्रशंसा में कहता है:
“वह युद्ध की विपत्ति में कठोर है, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता है, वह नंगी तलवार की तरह इरादे का पक्का है।”
हियाज - क्रोध और रोष के अर्थ में आता है और युद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कवि कहता है:
“प्रत्येक व्यक्ति युद्ध में उन्हीं उपकरणों के साथ जाता है, जो उसने इकट्ठा कर रखा है।”
मग़ज़ीयह - वास्तविक अर्थ क्रोध और आक्रोश है और आमतौर पर युद्ध के लिए उपयोग किया जाता है। इब्ने अनितमा ने युद्ध के लिए मग़ज़ीयह सब्द का प्रयोग किया है:
अरब के कवियों ने युद्ध की तुलना मेढ़ों के टक्कर लड़ने से भी की है। तो इसके लिए वे “निताह” शब्द का प्रयोग करते हैं। साद बिन मलिक कहता है:
“जब कोई अचानक आगे बढ़कर दुश्मन से लड़ना पसंद नहीं करे, तो बचने के बाद वापस मुड़ना बेहतर होता है।
युद्ध की तुलना ऊँट की छाती से की गई है, क्योंकि जब ऊँट अपनी छाती किसी चीज़ पर रख देता है, तो वह चीज़ पिस कर रह जाती है, और इसलिए भी कि ऊँट एक द्वेषपूर्ण और प्रतिशोधी जानवर है। कवि कहता है:
“तुमने एक बार हमारे ऊपर ऊँट की छाती को रख दिया है, इसलिए हम भी जल्द ही उसे तुम्हारे ऊपर डाल देंगे।”
युद्ध की तुलना चक्की से की गई है, क्योंकि यह भी शत्रु को आटे की तरह पीस कर रख देता है। अबुल ग़ौल तहवी कहता हैं:
“वे इतने वीर हैं कि भयंकर युद्ध की चक्की चलते समय उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता।”
अम्र बिन कुलसूम कहता है:
“जब हम अपनी चक्की को लेकर किसी क़ौम की ओर जाते हैं, तो उस युद्ध में उसका आटा बन जाता है।”
युद्ध के लिए “चक्र” का रूपक भी इस्तेमाल किया गया था। अंतरा बिन शद्दाद अबसी कहता है:
“मुझे डर है कि ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं और ज़मज़म के दोनों बेटे लड़ाई के चक्र में आ जाएं।”
युद्ध की तुलना प्राय: अग्नि से भी की गई है, क्योंकि वह भी शत्रु को अग्नि के समान भस्म कर देता है। हारिस बिन हिल्ज़ाह कहता है:
“हम धूल से परेशान न हुए, जब कि सवार तितर-बितर होकर भाग गए, और लड़ाई की आग ख़ूब भड़क उठी।”
साद बिन मलिक कहता है:
“कोई युद्ध की आग से मुंह मोड़ जाए, तो मोड़ जाए, मैं तो क़ैस का बेटा हूं, मैं कभी नहीं हटूंगा।”
इन सब उपमाओं और लोकोक्तियों से ज्ञात होता है कि युद्ध अरबों की कल्पना में एक ऐसी चीज़ का नाम है, जिसमें लूट-खसोट हो, शोर-शराबा हो, क्रोध और हिंसा हो, जिसके विरुद्ध यह लड़ी जाए, उसका दमन कर दे और उसे इस तरह बर्बाद कर छोड़े कि उसके भय से शरीर कांपने लगे। उनकी कल्पना में दो लड़ते हुए शत्रु उन मेंढ़ों के समान हैं, जो क्रोधित होकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ते हैं । ऐसे युद्ध में साहस और वीरता तो अवश्य है, पर नैतिक श्रेष्ठता और मानवीय गरिमा का नाम भी नहीं है।
अरबों के चरित्र पर सशस्त्र संघर्ष की आवृत्ति का प्रभाव
युद्ध अरबों के दिलों में सबसे वांछित चीज़ थी। उनमें आम धारणा यह थी कि अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा मरता है, तो उसकी आत्मा उसकी नाक से निकलती है, और अगर वह युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरता है, तो उसकी आत्मा शरीर के घावों से बाहर आती है। हर अरब की यही कामना थी कि उसकी आत्मा उसके घाव से बाहर आए, क्योंकि वह आत्मा के नाक से बाहर निकलने को घोर लज्जा की दृष्टि से देखते थे।
अरब कवि गर्व से कहते हैं कि उनमें से कोई नाक की मौत नहीं मरता है। एक कवि अपने राष्ट्रीय गौरव का वर्णन करते हुए कहता है:
युद्ध की आहट सुनते ही अरब समाज के लोगों का दायित्व था कि वे शस्त्र लेकर दौड़ पड़ें और यह न पूछें कि युद्ध कैसा है और क्यों लड़ा जा रहा है? युद्ध का कारण चाहे कुछ भी हो, उस से बचना, बड़ी कायरता का विषय माना जाता था। अगर किसी का समुदाय इस प्रकार की कायरता दिखाता, तो वह बड़ी लज्जा और अपमान की बात समझी जाती थी। इसके बारे में एक कवि कहता है:
“बनू माज़न की हालत यह है कि जब उनका कोई भाई मुसीबत और पीड़ा के समय उन्हें मदद के लिए बुलाता है, तो वे कारण पूछे बिना युद्ध में कूद पड़ते हैं।”
“काश मुझे ऐसी क़ौम मिलती जो घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर जम कर हिंसा करती।”
एक अन्य कवि अपने कुल की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है-
“मैं उस क़ौम से हूं जिसके लोग वीरों के ललकारने पर मर मिटे।”
इस्लामपूर्व अरब का साहित्य इस प्रकार की भावनाओं से भरा पड़ा है, जिसके अध्ययन से पता चलता है कि अरब लोग युद्ध को बड़ी शान समझते थे और उनकी दृष्टि में रक्तपात एक महान पुण्य का कार्य था।
युद्ध के कारक
विजय-धन की चाहत
एक चीज़ जो उन्हें इस भयानक काम के लिए प्रेरित करती थी, वह थी, विजयधन या लूट के माल की चाहत। जब एक अरब हथियार उठाता, तो उसके मन में जो पहली इच्छा उठती वह यह होती कि युद्ध में उसे बहुत सा लूट का माल और ग़ुलाम मिलें। व्यापार या श्रम द्वारा अर्जित धन उनकी दृष्टि में एक अपमानजनक धन था, उनकी दृष्टि में वास्तविक सम्मान उस धन की प्राप्ति में था जिसे वे युद्ध के मैदान से लूट कर लाते थे। वे कई बार ऊँट, बकरियों, दासों और लूट के अन्य मालों के जुनून में युद्ध छेड़ दिया करते थे। एक कवि लूट के लिए अपने जुनून को इस तरह व्यक्त करता है:
“अगर मैं जीवित रहा तो ऐसे युद्ध पर जाऊँगा जिसमें मुझे लूट का बहुत सा माल मिले।”
“जब हमारे घोड़े किसी क़बीले पर हमला करते हैं, और उन्हें वहां कुछ लूट का माल नहीं मिलता, तो वे ज़बाब और ज़ब्बा पर टूट पड़ते हैं, जो कि अपने घरों में सो रहे होते हैं,फिर जो मरता है, मर जाए, उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। और कभी-कभी जब हमें लूट के लिए कोई और नहीं मिलता है तो हम ख़ुद अपने भाई पर हमला कर बैठते हैं ।”
जब कोई क़बीला युद्ध के लिए जाता था, तो उसकी औरतें अपने आदमियों से संकल्प लेती थीं कि लूट का माल लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे। तो अम्र बिन कुलसूम कहता है:
“उन्होंने अपने पतियों से वचन लिया कि जब वे शौर्य के चिह्न धारण कर शत्रु सेना से मिलें तो घोड़े और चमकती तलवारें, और रस्सियों से बंधी दासियां ले कर लौटें।”
लूट की इस लालसा में, अक्सर ऐसा होता था कि जब कोई सेना किसी क़बीले पर हमला करने के लिए निकलती थी, तो बहुत से लोग केवल माल की लूट के लिए उसमें शामिल हो जाते थे। हरिथ बिन हिलज़ा एक क़ौम पर चढ़ाई का वर्णन करते हुए कहता है:
“उसकी सहायता के लिए हर क़बीले के भूखे लुटेरे इकट्ठा हो गए, जैसे कि वे चील हों।”
फिर आगे कहता है:
“फिर हम ने बनू तमीम पर आक्रमण किया और हराम महीने में पहुंच कर उनकी बेटियों को दासियां बना लिया।”
यह लूट-मार अरबों के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, और अरब बुद्धिमान लोग उस युद्ध को बेकार और व्यर्थ मानते थे, जिसमें कुछ धन की प्राप्ति न हो। ऐसा ही एक ज्ञानी कहा करता था, “सबसे अच्छी जीत वह है जिसमें बहुत से क़ैदी हाथ आएं और सबसे अच्छी लूट वह है, जिसमें ऊँट और बकरियां मिलें।”
गौरव
लूट-पाट के साथ-साथ दूसरा महत्वपूर्ण प्रेरक अपनी प्रतिष्ठा और वीरता के प्रदर्शन की इच्छा थी। गौरव की यह भावना वास्तव में अरबों की स्वाभाविक विशेषताओं में से एक थी। वे अपने जैसे लोगों की तुलना में ख़ुद को शक्तिशाली, विशिष्ट और सम्मानित साबित करने के लिए हर तरह के जोखिम उठाने को तैयार रहते थे। एक बहादुर अरब की सबसे बड़ी इच्छा यह होती थी कि दूसरे का ऊँट उसकी चरागाह में न चर सके। कोई उस जलस्रोत पर न आ सके जहाँ से वह पानी पीता है, जहाँ वह रहता है वहां दूसरों के लिए जगह न हो, जैसे कपड़े वह पहनता है, कोई और न पहन सके, उसकी तुलना में किसी को बड़ा और महान न माना जाए, उसके सामने किसी की प्रशंसा न की जाए, वह जिसे चाहे मार डाले, कोई उससे ख़ून का बदला न ले सके। उसका हाथ सबके ऊपर रहे, वह हर प्रकार से दूसरों पर श्रेष्ठ हो, कोई उसके सामने सिर न उठा सके। अंधकार युग के कवियों के काव्य ऐसी ही भावनाओं के वर्णन से भरे पड़े हैं:
“संसार के सभी क़बीले, जब से वे ज़मीन पर बसे हैं, जानते हैं कि, हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसे रोक देते हैं और जहां चाहते हैं वहां ठहरते हैं। जब हमारी बात मानी जाती है, तो हम रक्षा करने वाले बन जाते हैं और जब हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम एक जलस्रोत तक पहुँचते हैं, तो हम साफ़ पानी पीते हैं, और दूसरों को गंदा, कीचड़युक्त पानी पीना पड़ता है।”
हजर बिन ख़ालिद सअलबी गर्व के स्वर में कहता है:
“हमने अपनी सुरक्षित चरागाहों को दूसरों के लिए बंद कर रखा है और हमारे भालों ने दूसरों की सुरक्षित चरागाहों को, जिनपर शक्तिशाली पहरेदारों तैनात हैं, अपने लिए वैध बना लिया है।”
अखनस अपनी क़ौम की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है:
“मैं देखता हूं, कि हर एक क़ौम ने अपके ऊंटों की रस्सी छोटी रखी है, परन्तु हम ने उसे खुला छोड़ दिया है, और वह आज़ादी चरता-फिरता है।”
एक दूसरा कवि कहता है:
“अगर हम किसी की हत्या कर दें तो किसी क़बीले के लोगों में हमसे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं।”
इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इस्लामपूर्व अरब में हुई अधिकांश भयानक लड़ाइयां इसी झूठे गौरव की भावना का परिणाम थीं। बिसवस्स की प्रसिद्ध लड़ाई, जो बनू तग़लब और बनू बक्र बिन वायल के बीच पूरे 40 वर्षों तक चली, केवल इतनी सी बात पर हुई कि बनू बक्र बिन वायल के एक मेहमान का ऊँट बनू तग़लाब के मुखिया कुलैब बिन रबीया की चरागाह में चला गया था और कुलैब के ऊँटों के साथ चरने लगा था। कुलैब का नियम था कि वह अपनी चरागाह में किसी के जानवर को नहीं चरने देता था, न वह अपने आखेट के मैदान में किसी को शिकार खेलने देता, न किसी के पशुओं को अपने पशुओं के साथ पानी पीने देता, यहां तक कि किसी की आग को अपनी आग के सामने जलता हुआ भी नहीं देखता। उसने जब एक नए ऊंट को अपने ऊंटों के साथ चरते देखा तो क्रोधित हो उठा और उस पर एक तीर चला दिया, जो उसके थन में जा लगा। ऊँट के मालिक ने जब उसे घायल देखा, तो चिल्लाया, कि यह कैसा अपमान है। इस पर बनी बक्र में से एक युवक ने जाकर कुलैब की (जो उसका सगा बहनोई था) हत्या कर डाली। कुलैब के भाई को पता चला तो वह बदला लेने को उठ खड़ा हुआ, और दोनों क़बीलों में ऐसी हिंसा फूट पड़ी, कि जबतक दोनों बर्बाद नहीं हो गए लड़ते रहे।
एक और लड़ाई जिसे हर्ब दाहिस के नाम से जाना जाता है, केवल इसलिए लड़ी गई कि एक घुड़दौड़ में एक घोड़ा दूसरे घोड़े से आगे निकल गया। बनी अबस के प्रमुख, क़ैस बिन ज़ुहैर, के पास दाहिस और हिबरा नाम के दो घोड़े थे, जिनकी गति अरब में प्रसिद्ध थी। बनी बद्र के प्रमुख हुज़ैफ़ा बिन बद्र को क़ैस के घोड़े की प्रसिद्धि से इर्ष्या होने लगी। उसने अपने दो घोड़ों के साथ यह शर्त लगाई कि जिसके घोड़े आगे निकलें वह सौ ऊंट ले ले। शर्त के अनुसार दोनों के घोड़े दौड़ाए गए। जब दाहिस आगे निकलने लगा, तो हुज़ैफ़ा के एक आदमी ने उसके चेहरे पर वार कर उसे एक घाटी की ओर मोड़ दिया। इसी बात को लेकर पक्षों में विवाद हो गया। क़ैस ने हुजैफ़ा के बेटे नदबा को मार डाला। हुज़ैफ़ा ने कैस के भाई मलिक को मार डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि बनू अबस और बनू बद्र के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो आधी शताब्दी तक चलता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि दोनों पक्षों के घोड़ों और ऊँटों की नस्ल विलुप्त होने के क़रीब नहीं आ गई।
औस और ख़ज़रज की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ, जो पूरी शताब्दी तक चलती रहीं, घमंड और प्रतिद्वंद्विता की एक बहुत ही तुचछ घटना से शुरू हुई थी। बनी साद का एक व्यक्ति ख़ज़रजी सरदार मलिक बिन इजलान के पड़ोस में रहता था। एक बार उसने बनी क़ैनक़ाह के बाज़ार में दावा किया कि मेरा सहयोगी मलिक बिन इजलान सबसे श्रेष्ठ है। यह बात औस जनजाति के एक व्यक्ति को बहुत बुरी लगी और उसने ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को मार डाला। इस पर औस और ख़ज़रज के बीच हत्याओं और ख़ून-खराबे का ऐसा भयानक सिलसिला शुरू हो गया कि अगर इस्लाम न आया होता तो दोनों क़बीले लड़ते-लड़ते ख़त्म हो जाते।
फ़िजार की आख़िरी लड़ाई, जिसके बारे में इब्न असीर कहता है कि अय्यामे अरब में इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई, वह भी इसी घमंड की भावना का परिणाम थी। नुबूवत से 26 वर्ष पहले हैरा के राजा नुअमान बिन मुंज़र ने उकाज़ के बाज़ार में एक व्यापार कारवां भेजने की योजना बनाई और अरब प्रमुखों से पूछा कि इसे अपने संरक्षण में लेने की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। बराज़ बिन कैस कनानी ने कहा कि मैं उसे बनी कानाना से सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी लेता हूं। हवाज़िन के एक सरदार उरवतुल रहाल ने कहा कि मैं उसे सभी अरबों से सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी लेता हूं। बराज़ इस दावे को सहन नहीं कर सका और जब उरवा कारवां को साथ लेकर चला, तो उसने रास्ते में उरवा की हत्या कर दी। इस घटना ने कानाना और हवाज़िन के बीच दुश्मनी को फिर से बढ़ा दिया। दोनों कुलों में युद्ध छिड़ गया। क़ुरैश ने कानाना का पक्ष लिया और बनू सक़ीफ़ ने हवाज़िन का पक्ष लिया। चार साल तक भारी रक्तपात जारी रहा और यौमुल शमता, यौमुल इबला, यौमुल शर्ब और यौमुल हरीरा के भयानक नरसंहार हुए, जिसने अरब की पिछली सभी लड़ाइयों को भुला दिया।
प्रतिशोध
एक और शक्तिशाली मक़सद जिसने अरब इतिहास को ख़ून से रंग दिया था, बदले की भावना थी। अरबों का मानना था कि जब किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, तो उसकी आत्मा एक पक्षी का रूप धारण कर लेती है और तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका बदला नहीं ले लिया जाता। उनकी शब्दावली में इस पक्षी का नाम हामा या सदाअ था।
कुछ लोगों का मानना था कि जिसका बदला ले लिया जाता है वह जीवित रहता है और जिसका बदला नहीं लिया जाता वह निर्जीव हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि जब तक बदला नहीं लिया जाता तब तक मृतक की कब्र में अंधेरा रहता है। ऐसी मान्यताओं के आधार पर मृतक के परिजन, कुल के सदस्य, यहां तक कि उसके क़बीले के सहयोगी भी उसके हत्यारे से ख़ून का बदला लेकर उसकी आत्मा को संतुष्ट करना अपना दायित्व समझते थे। अगर हत्यारा उससे निम्न स्तर का व्यक्ति था, तो उसके क़बीले के ऐसे व्यक्ति को मारने का प्रयास किया जाता था, जिसका ख़ून वे मृतक के ख़ून के बराबर मानते थे। इस प्रकार कभी-कभी किसी व्यक्ति के मारे जाने पर बड़े-बड़े कुलों में युद्ध की ज्वाला भड़क उठती थी और ऐसा रक्तपात मचता था कि वर्षों तक नहीं रुकता था। अगर कोई व्यक्ति या जनजाति अपने आदमी के ख़ून का बदला लेने में आनाकानी करती या इसके बदले में हरजाना स्वीकार कर लेती, तो यह बहुत ही अपमान की बात मानी जाती थी।
इस्लामपूर्व अरब के कवियों की कविता में बहुतायत से दिखाई देने वाले विषयों में से एक बदला लेने की उन की मान्यता भी है। इस विश्वास के आधार पर, वे क़बीलों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे और कई कवि गर्व से कहते हुए नज़र आते हैं कि उनके क़बीले ने कभी भी अपने मारे गए लोगों के ख़ून को व्यर्थ नहीं जाने दिया। समवाल बिन आद कहता है:
“हम में से कोई भी मुखिया अपनी नाक से नहीं मरा, और जब हमारा कोई आदमी मारा गया, तो उसका ख़ून कभी बेकार नहीं गया।”
हारिस बिन हिलज़ा कहता है:
अगर तुम मल्हा से साकिब तक कब्रों को खोदोगे, तो देखोगे कि दफ़नाए हुए कुछ लोग मुर्दा हैं, (जिनका ख़ून व्यर्थ गया, और वे तुम में से हैं) और कुछ जीवित हैं (जिनका बदला ले लिया गया और वे हम में से हैं)।”
एक कवि अपनी स्तुति का वर्णन करते हुए कहता है:
“जब उन्हें ख़ून का हर्जाना लेने और लड़ाई करने के बीच चुनाव का अधिकार दिया जाता है, तो वे मौत की कामना करते हैं।”
बनी असद के एक शायर अपने क़बीले को वसीयत करता है:
“मेरे ख़ून के बदले में दुश्मन से हर्जाना न ले लेना, क्योंकि क़र्ज़ बना रहता है और हर्जाना का धन ख़र्च हो जाता है।”
बनू ख़ुज़ाआ का एक शायर अपने क़बीले को इस तरह बदला लेने के लिए प्रेरित करता है:
“हर्जाना के रूप में वे जो कुछ भी देते हैं, उसका विचार भी मन में न लाओ, वह तुम्हारे लिए ज़हर है।”
एक कवि कहता है:
“अगर तुमने मेरे ख़ून का बदला नहीं लिया और धन स्वीकार कर लिया, तो तुम कनकटे शुतुरमुर्ग की तरह अपमानित फिरो।”
ये अरब क़बीलाई दुश्मनी और लड़ाइयों की असली प्रेरणाएँ हैं, इनमें किसी महान और उच्च उद्देश्य का नामोनिशान तक नहीं है। वही शुद्ध पाशविक और दानवी आवेग जो एक पशु को अपने शत्रुओं से भिड़ने के लिए, अधिक भयानक रूप में, उकसाता है। युद्ध उनके जीवन के विशुद्ध पशु पक्ष से संबंधित था, उसका मानवीय और दैवीय पक्ष से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि उनके दिमाग़ में यह अवधारणा मौजूद ही नहीं थी कि युद्ध का मानव जाति के उच्च नैतिक पहलू से भी कोई लेना-देना हो सकता है।
युद्ध में बर्बरता
जिस तरह इस्लामपूर्व अरब की युद्ध की अवधारणा बहुत नीच थी और जिस तरह युद्ध के लिए उनके मक़सद भी नीच और अशुद्ध थे, उसी तरह उनके युद्ध में बर्बरता भी चरम पर थी। उनके दिमाग़ में युद्ध की विशेषता यह थीं कि यह भयानक होना चाहिए, इसमें क्रोध और रोष की पूरी अभिव्यक्ति हो, पीड़ा भरी चीख़ और पुकार हो, दमन का चक्र हो, आग और ख़ून हो और दुश्मन के लिए बचाव का कोई रास्ता न हो। इसलिए युद्ध में उनके कार्य भी इसी अवधारणा के अनुसार थे। उनके लिए, एक राष्ट्र के ख़िलाफ़ हथियार उठाने का मतलब किसी भी तरह से उसे अपमानित करना और नष्ट कर देना था। उनका संघर्ष किसी प्रकार की नैतिक सीमाओं से अवगत न था। वह केवल एक ही बात जानता था और वह यह कि दुश्मन को मार कर ही दम लेना है। इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए तरीक़ों का विवरण इस्लामपूर्व अरब की किताब और अरब इतिहास में बहुतायत से मिलता है, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया गया है।
ग़ैर-लड़ाकों पर हमला
युद्ध में लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच कोई अंतर नहीं था। शत्रु राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को शत्रु माना जाता था और युद्ध का दायरा सभी वर्गों और दलों पर समान रूप से फैला हुआ था। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों, घायलों, किसी को भी इस से छूट नहीं थी। बल्कि शत्रु राष्ट्र को अपमानित करने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से हिंसा और उत्पीडण का शिकार बनाया जाता था। विजित राष्ट्र की स्त्रियों का अपमान करना विजेता के गौरव में से एक माना जाता था और कवि बड़े गर्व के साथ इसका उल्लेख करते थे। एक कवि कहता है:
“बहुत सी शरीफ़ महिलाएं, जिनके ग़ैरत वाले पति उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करते थे, मैंने उनके टख़नों को खोल दिया।”
एक और कवि कहता है:
“उस समय असली लक्ष्य गोरी-गोरी पर्दानशीं महिलाएं होती हैं, न कि चरागाह से लौट रहे ऊंट।”
अम्र बिन कुलसूम युद्ध में बहादुरी से लड़ने का कारण यह बताता है कि उसके क़बीले को अपनी महिलाओं के अपमानित होने का खटका लगा हुआ है। कहता है:
“हमारे पीछे गोरी-गोरी सुंदर महिलाएं हैं। हमें डर है कि कहीं वे विभाजित या अपमानित न हो जाएं।”
कभी-कभी तो ग़ुस्से में दुश्मन की औरतों के पेट तक को चीर दिया जाता था। इस प्रकार, इब्ने तुफैल, फ़ैफ़ अल-रीह की लड़ाई में अपने क़बीले की जीत का उल्लेख करते हुए कहता है:
“हम ने फ़ैफ़ अल-रीह में नाहद और शुख़म पर भारी प्रहार करने के बाद अपने उत्साह में गर्भवती महिलाओं के पेट चीर डाले।”
आग की यातना
शत्रु को प्रताड़ित करने और हानि पहुँचाने का अधिकार अप्रतिबंधित था, यहाँ तक कि वे आग की यातना देने से भी नहीं हिचकते थे। अरब इतिहास की यह प्रसिद्ध घटना है कि यमन के राजा जुनवास ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया जो उसके धर्म से फिर गए थे और उन्हें धधकती आग में फेंक दिया। पवित्र क़ुरआन में भी उस धटना का उल्लेख किया गया है।
जब मुंज़िर बिन इमराउल-क़ैस ने ऊवारह की लड़ाई में बनी शैबान पर जीत हासिल की, तो उसने उनकी महिलाओं को ज़िंदा जलाना शुरू कर दिया और बनी क़ैस के एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान छुडवाई। आशा उसी घटना के बारे में गर्व से कहता है:
“उसने ऊवारह की लड़ाई में बनी शैबान के बंदियों को छुड़ा लिया, जबकि उनकी युवा लड़कियों को आग में फेंका जा रहा था।”
अम्र बिन मुंज़िर ने एक ग़लती के आधार पर बनी दारिम के सौ आदमियों को ज़िंदा जलाने की मन्नत मानी थी। इसलिए उस ने उन पर चढ़ाई करके उनके 99 पुरूषों को पकड़ लिया, जिन्हें उस ने ज़िन्दा जला दिया। अब मन्नत पूरी करने में एक ही कमी रह गई थी। संयोगवश उस समय किसी दूसरी जाति का एक व्यक्ति उधर से गुज़र रहा था। उसने खाना पकते देखा तो अम्र बिन मुंज़िर की सेना की ओर आ गया। अम्र ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उसे ही आग में झोंक दिया। जरीर उसी घटना के बारे में कहता है:
“कहाँ हैं वे जो अम्र की आग में भस्म हुए थे, और असद कहाँ है, जो तुम्हारे बीच में पाला गया था।”
युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार
युद्ध में बंदियों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था और कभी-कभी उन्हें प्रतिशोध की आग में अत्यधिक यातनाएं देकर मार दिया जाता था। उकुल और उरैना की घटनाएं हदीसों में दर्ज हैं, वे नबी (सल्ल.) के चरवाहों को पकड़ कर ले गए, उनके हाथ-पैर काटे, उनकी आंखें फोड़ दीं और उन्हें तपती रेत पर फेंक दिया, यहां तक कि विवशता की हालत में उनकी मौत हो गई।
ऊवारह की लड़ाई की घटना प्रसिद्ध है कि बनी शैबान के जितने भी बंदी मुंज़िर बिन इमराउल-क़ैस के हाथ आए, उसने ऊवारह पर्वत की चोटी पर बैठाकर उनकी हत्या करना शुरू कर दिया और कहा कि जब तक उनका रक्त पहाड़ की जड़ तक न बह जाए मैं हत्याओं की श्रृंखला को नहीं रोकूंगा। अंत में, जब मृतकों की संख्या सैकड़ों से अधिक हो गई, तो मजबूर होकर उसने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ख़ून पर पानी डलवा दिया और वह बह कर पहाड़ की जड़ तक पहुंच गया। (इब्ने असीर)
इमराउल-क़ैस के पिता हजर बिन हारिस ने जब बनी असद पर हमला किया, तो उनके जितने लोग भी पकड़े गए सभी की उसने हत्या करा दी और आदेश दिया कि तलवारों से नहीं बल्कि लाठियों से मार-मार कर उनकी हत्या की जाए। (इब्ने असीर)
अप्रत्याशित आक्रमण
दुश्मन पर युद्ध की घोषणा किए बिना ग़फ़लत की स्थिति में, सुबह होने से पहले उन पर टूट पड़ने को सबसे साहसी युद्ध रणनीति में से एक माना जाता था। क़ुर्रा बिन ज़ैद कहता है:
क़ैस बिन आसिम एक सेना के साथ सुबह के समय उनके पास जा पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं पाया, सिवाय इसके कि भाले के तीर छाती के पार हो रहे थे।
अब्बास बिन मर्दास कहता है:
“मैंने उस क़बीले जैसा क़बीला कभी नहीं देखा, जिस पर हमने सुबह हमला किया, और न ही हमारे जैसा कोई था, जब हमने शूरवीरों का सामना किया।”
इसलिए लोग अपने दोस्तों को दुआ देते थे कि ''तुम सुबह के समय सकुशल रहो।''
अरब में शत्रु सेनापतियों को रात में नींद में ही मार डालने की भी प्रथा थी। इसे “फ़तक” कहते थे और ऐसा करने वाले को “फ़ताक” कहा जाता था। हारिसा बिन ज़ालिम अलमरी, बराज़ बिन क़ैस अलकनानी और सलीक बिन सिल्का, अरब के प्रसिद्ध फ़ताक गुज़रे हैं।
मृतकों का अपमान
बदला लेने के जुनून में दुश्मन के शवों तक का अपमान करने से भी वे पीछे नहीं हटते थे। शवों के नाक, कान और दूसरे अंगों को काटकर, जीवितों का बदला मृतकों से लिया जाता था। कभी-कभी ऐसी बर्बरतापूर्ण हरकतें भी की जाती थीं कि सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उहुद की लड़ाई की मशहूर घटना है कि क़ुरैश की औरतों ने इस्लाम के शहीदों के नाक, और कान काट कर हार बना लिए। अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद ने सैयदना हमज़ा की किडनी निकाल कर चबा ली थी। एक लड़ाई में जब बनू जदीला के प्रमुख इस्बा बिन अम्र को मार दिया गया था, बनू सिनबस के एक व्यक्ति ने उसके दोनों कान काट कर अपने जूते में चिपका लिए। अबू सरवह, सिनबसी उसी पर गर्व करते हुए कहता है:
“हम तुम्हारे कानों का पैबंद अपने जूतों में लगाते हैं।”
एक अन्य कवि कहता है:
“अगर तुम अपने मन में हम से द्वेष रखते हो, तो यह बुरा नहीं है, क्योंकि हम ने तुम्हारे नाक और कान काट डाले, और तुम्हें पकड़-पकड़ कर बेच डाला है।”
जब किसी व्यक्ति से घोर शत्रुता होती थी तो वे शपथ खाकर कहते थे कि हम उसे मार डालेंगे और उसकी खोपड़ी में शराब पीयेंगे। उहुद की लड़ाई में, दो भाई, मुसाफ़ा बिन तलहा और जलास बिन तलहा, असिम बिन साबित द्वारा मारे गए थे। दोनों की मां सलाफा ने क़सम खाई थी कि वह आसिम की खोपड़ी में शराब पीयेगी। जब आसिम मक़ाम राजी में शहीद हो गए, तो क़ुरैश के लोग सलाफा के हाथों उनका सिर बेचने के लिए उनकी तलाश में गए (इस घटना का उल्लेख तबकात इब्न साद, फ़त्हुल-बारी और असद अल-ग़ाबह में किया गया है)। हर्बुल-फ़साद (जो 25 साल तक चला) में, समुदायों ने अक्सर एक-दूसरे के मृतकों की खोपड़ी में शराब पी। इसी तरह की घटनाएं जंग यहामीम में भी हुईं। इसलिए, अबू सरवह इनही की ओर इशारा करते हुए कहता है:
“हम अनिच्छा से तुम्हारी खोपड़ी में शराब पीते हैं।”
शत्रुओं की लाशों को मांस खाने वाले जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था और यह उनके लिए गर्व की बात थी।अंतरा कहता है:
“अगर वे मेरी निन्दा करते हैं, तो कुछ ग़लत नहीं करते, क्योंकि मैं ने उनके पिता को बनैले पशुओं का आहार बनने के लिए छोड़ दिया है।”
आतिका बिन्त अब्दुल-मुत्तलिब, हर्बे फ़िजार की घटनाओं के बारे में शैखी बघारते हुए कहती है:
हमारे घुड़सवारों ने मलिक को ज़मीन पर पड़ा छोड़ दिया और उसे बनैले पशु नोच-नोच कर खाते थे।”
हर्बे बिसवस का उल्लेख करते हुए एक कवि कहता है:
“उन मृतकों पर कौवों और गिद्धों के झुंड के झुंड आते हैं और उनके हाथों को नोच-नोच कर खाते हैं।”
विश्वासघात
इस्लामपूर्व अरब के युद्ध में समझौता के प्रति वफ़ादारी का भी कोई महत्व नहीं था। दुश्मन से बदला लेने का जब भी अच्छा मौक़ा आया, सारे वादे टूट गए। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ख़ुद पैग़म्बर (सल्ल.) के समय में अवज्ञाकारी अरबों के वचनभंग की घटनाएं बार-बार हुई हैं। इस्लाम के पैग़म्बर ने बनू क़ैनक़ाह, बनू नज़ीर, बनू क़ुरैज़ा के साथ समझौते किए थे, लेकिन तीनों ने उन्हें तोड़ दिया। बनू नज़ीर ने ख़ुद नबी (सल्ल.) को जान से मारने की साज़िश रची थी। बनू क़ुरैज़ा ने खुलेआम इस्लाम के ख़िलाफ़ ग़ज़वा अहज़ाब (समुदायों के युद्ध) में भाग लिया। बनू क़ैनक़ाह ने क़ुरैश के उकसाने पर सबसे पहले युद्ध की घोषणा की। रअल और ज़कवान के क़बीलों ने स्वयं अल्लाह के रसूल से कुछ पुरुषों को सहायता के रूप में मांगा था, और जब आपने उनके लिए सहाबियों का एक समूह भेजा, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उन सभी को मार डाला। बनू लहयान ने हज़रत ख़ुबैब, ज़ैयद बिन विश्नाह और अब्दुल्लाह बिन तारिक़ को राजीअ में पनाह दी और जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन्होंने तीनों को पकड़ कर बांध दिया, एक को मार डाला और दो को मक्का ले जाकर बेच दिया। इसी तरह के विश्वासघात के बारे में पवित्र क़ुरआन में कहा गया है कि वे किसी मुसलमान के साथ रिश्तेदारी या समझौते को नहीं मानते हैं।
इस्लामपूर्व अरब के युग में अरबों के युद्ध का ये तरीक़ा आम था। एक कवि ने अरब सेना की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार किया है:
“मैं एक सभ्य नागरिक नहीं हूं अगर तुम्हारे घरों के सामने फाड़ने और पीसने वाली सेना न आए।”
“उसे देखते ही बलवान दब जाते हैं और भय के गर्भवती के गर्भ गिर जाते हैं।”
जवान कुँवारियाँ उसके भय से बूढ़ी हो जाती हैं, और वे भी उसके भय से भाग जाते हैं, जो अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते।”
(2) रोम और ईरान की युद्ध पद्धतियाँ
ये अरब तो बर्बर थे, उनके पास सभ्यता और संस्कृति का नाम तक नहीं था, ये ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल से परिचित नहीं थे। उनमें ऐसी हिंसा और दानवता मौजूद थी तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन देखना यह है कि उस युग में जो राष्ट्र सभ्यता के आकाश पर पहुँच चुके थे, उनकी स्थिति क्या थी।
इतिहास ने उस अवधि की लड़ाइयों के बारे में बहुत सी जानकारियां संरक्षित की हैं। जिन लोगों ने उनका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि कम से कम इस संबंध में सभ्य और असभ्य दुनिया के व्यवहार में कोई बहुत अंतर नहीं था। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता तो वह उसका सफ़ाया कर डालने का ही निश्चय करता था। लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं था। शत्रु राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हत्या का पात्र समझा जाता था। महिलाएँ, बच्चे, वृद्ध, घायल, रोगी, साधु, सन्यासी, सभी दुश्मन और हत्या के पात्र समझे जाते थे । शत्रु की फ़सलों और बगीचों को नष्ट करना, इमारतों को तोड़ना, लूटपाट करना और बस्तियों को आग लगा देना सेनाओं की कार्रवाई में एक सामान्य बात थी। उग्र प्रतिरोध के बाद किसी शहर का हार जाना, उस शहर के लिए मौत का संदेश था। जब क्रोधित विजेता उसमें प्रवेश करते थे, तो वे खुलेआम नरसंहार शुरू कर देते थे और जब उससे भी उनकी बदले की आग ठंडी नहीं होती, तो वे शहर में आग लगा देते थे। हद तो यह है कि सिकंदर ‘महान’ भी का सिद्धांत भी इससे अलग नहीं था। जब उसने 6 महीने की गंभीर घेराबंदी के बाद सीरिया के प्राचीन व्यापारिक केंद्र सौर पर विजय प्राप्त की, तो, अत्यंत ग़ुस्से में आकर नरसंहार का आदेश जारी कर दिया, और उस राष्ट्र के लोगों ने, जिसे उस युग में दुनिया का सबसे सभ्य राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था, 8 हज़ार निर्दोष लोगों को मार डाला और लगभग 30 हज़ार सभ्य नागरिकों को ग़ुलाम बनाकर बेच डाला। उस युग में युद्धबंदियों के लिए हत्या और ग़ुलामी के सिवा कोई तीसरा विकल्प नहीं था। कभी-कभी जब वे शत्रु शासकों और उन के सेनानायकों पर प्रभुत्व पा लेते तो घोर अपमान के साथ प्रताड़ित कर के उन्हें मार डालते।
राजदूतों का सम्मान युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है, लेकिन उस युग में यह समूह भी दुर्व्यवहार से सुरक्षित नहीं था। किसी राजा के दरबार में विरोधी पक्ष की ओर से ऐसा सन्देश ले कर आना, जिसे राजा अपना अपमान और अपने गौरव के विरुद्ध समझता हो, राजदूत के लिए अपनी मृत्यु का सन्देश ले जाने के समान था। ऐसे अवसरों पर राजदूतों को अपमानित करना और उन्हें क़ैद कर लेना असामान्य नहीं था, और कभी-कभी तो उन्हें सीधे मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। सबसे ज़्यादा मुसीबत धार्मिक समुदाय के लिए थी। अगर, दुर्भाग्य से, विजित देश के निवासी दूसरे धर्म के अनुयायी होते, तो विजेता का पहला काम उनकी आस्था पर हमला करना, उनके पवित्र स्थानों को अपवित्र करना, बल्कि उन्हें ध्वस्त कर देना और धर्म से जुड़े लोगों को अपमानित करना होता। कभी-कभी जुनून इस हद तक बढ़ जाता था कि विजेता तलवारों के बल पर विजितों को अपने धर्म बदलने के लिए भी मजबूर करता था।
प्राचीन काल के सबसे सभ्य राज्य दो थे, एक रोम, दूसरा ईरान। सभ्यता, विज्ञान, आचार और वैभव, हर दृष्टि से उस काल में विश्व के सभी राष्ट्रों पर उनकी श्रेष्ठता थी, इसलिए उनके ही इतिहास पर दृष्टि डालें और देखें कि युद्ध में उनका व्यवहार कैसा था।
धार्मिक अत्याचार
रोम और ईरान के बीच राजनीतिक मतभेदों के साथ-साथ धार्मिक मतभेद भी थे। जब मजूसी (मगियन) ईरान और ईसाई रोम के बीच युद्ध होता और एक को दूसरे के देश पर आक्रमण करने का अवसर मिलता, तो धर्म को सबसे ज़्यादा अत्याचार और क्रूरता का निशाना बनाया जाता। क़ोबाद (501 से 531 ईस्वी) के समय में, जब हैरा के राजा मुंज़िर ने ईरानी सरकार के इशारे पर सीरिया पर आक्रमण किया, तो उसने एंटिओक में 400 ननों को पकड़ लिया और अपने देवताओं के लिए उनकी बलि चढ़ा दी। (History of Persia, Sykes, Vol. 1 page 482).
जब ख़ुसरो परवेज़ ने सीज़र मौरिस से बदला लेने के बहाने रोमन साम्राज्य के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की, तो उसने अपने क्षेत्र में ईसाई चर्चों को ध्वस्त करा दिया, चर्च की संपत्ति को लूट लिया और ईसाइयों को आग की पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया। (Gibbon, Roman Empire, vol.5, para XLVI)
615 में जब उसने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तो उसने वहां के मुख्य पादरी जकारियाह को बंदी बना लिया, उनका वह मूल क्रॉस लूट ले गया जिस पर ईसाइयों की मान्यता के अनुसार हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था, उनके बड़े आराधनालय सेंट हेलेना और ग्रेट कॉन्सटेंटाइन में आग लगा दी, धार्मिक स्मारकों और अन्य मूल्यवान चीज़ों को लूट लिया और 90 हज़ार ईसाइयों को या तो मार डाला या बंदी बना लिया। (E.A. Ford Byzantine Empire)
इसके प्रत्युत्तर में जब हरकुलिस ने उत्तर से ईरान पर आक्रमण किया तो उसने मागी के अग्निकुंडों को नष्ट कर दिया, पारसियों की मातृभूमि उर्मियाह को मिट्टी में मिला दिया और मजूसी (मगियन) धर्म का अपमान और तिरस्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। (Gibbon, Roman Empire, vol. 1, chapter XLVI)
रोमनों की शत्रुता में, स्वयं ईरान के ईसाई नागरिकों का गंभीर रूप से दमन किया जाता था। रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म अपनाने से पहले तक, ईरान के ईसाई सुरक्षित थे, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के बपतिस्मा के बाद, ईरान का अपने ईसाई नागरिकों के प्रति रवैया बदल गया। । 339 ईस्वी में शापुर जुलकताफ ने बिशप मारशिमोन और 105 अन्य पुजारियों को मार डाला और कई ईसाई चर्चों और मठों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद, 40 वर्षों तक ईसाइयों का अत्यधिक उत्पीड़न जारी रहा (Sykes vol. 1, page 448)
बहराम द्वारा मनविया सम्प्रदाय को नष्ट करने के लिए किए गए कठोर उपाय अत्यंत भयावह थे। जब मनी ने पारसी धर्म को छोड़कर अपने धर्म का आविष्कार किया और बहुत से लोग उसका अनुसरण करने लगे, तो बहराम ने आधुनिक धर्म के अनुयायियों की हत्या करानी शुरू कर दी और मानी को गिरफ़्तार करके मार डाला। उसकी खाल निकलवाई और उसमें भुस भरवा कर उसे नगर के मुख्य दरवाज़े पर लटका दिया। उस दरवाज़े को लंबे समय तक बाबे मानी (मानी का दरवाज़ा) के नाम से जाना जाता था (अल्लामा अल-बैरूनी ने अतहरुल-बकिया में इस घटना का उल्लेख किया है)।
दूतों पर अत्याचार
राजदूतों के सम्मान की अवधारणा उस समय भी सिद्धांत रूप में तो मौजूद थी, और राजनीतिक विचारक उस सम्मान का महत्व समझते थे, लेकिन व्यवहार में इसे बहुत कम माना जाता था। जब पर्शियन साम्राज्य के शासक अर्देशिर के राजदूत सीजर एलेक्जेंडर के दरबार में इस संदेश के साथ पहुंचे कि “रोमनों को केवल यूरोप से संतुष्ट रहना चाहिए और सीरिया और अनातोलिया को ईरानियों के लिए छोड़ देना चाहिए,” तो सीज़र बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन राजदूतों को क़ैद कर लिया। (Sykes vol. 1, page 426)
नौशेरवान जैसे प्रमुख राजा, जो अपने न्याय और सदव्यवहार के लिए प्रसिद्ध था, के दरबार में जब वेज़बिल अत्राक के राजदूत विरोध प्रस्ताव लेकर आए तो उसने प्रस्ताव का स्पष्ट उत्तर देने के बजाय उन्हें ज़हर देकर चुपचाप मार डालना अधिक उचित समझा। (वही, Vol.1, P-494)
जब ख़ुसरो परवेज़ की विजयी कार्रवाइयों ने एशिया और अफ्रीका, सीरिया, फ़िलिस्तीन, मिस्र और पूरे एशिया माइनर में रोमन साम्राज्य को लगभग समाप्त कर दिया, यहां तक कि ईरानी सेना कॉन्स्टेंटिनोपल के सामने Chalce Don तक पहुंच गई, तो ख़ुसरो के साथ शांति की गुहार लगाने के लिए हर्कुलिस ने अपने राजदूत भेजे, तो उसके जवाब में ख़ुसरो ने प्रतिनिधिमंडल के मुखिया की जीवित हालत में चमड़ी उतरवा दी, और प्रतिनिधिमंडल के बाक़ी सदस्यों को क़ैद कर लिया। फिर जवाब में हर्कुलिस को एक पत्र लिखवाकर भेजा, जिसका शीर्षक था: “श्रेष्ठ देवता और विश्व सम्राट ख़ुसरो की ओर से उसके मूर्ख और तुच्छ ग़ुलाम हर्कुलिस के नाम।” (Byzantine Empire, page 101)
विश्वासघात
समझौतों के सम्मान पर हमला करने में ये सभ्य राष्ट्र कम दुस्साहसी नहीं थे। उनके अनुसार ज़रूरत के सामने वचन कुछ भी नहीं था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब रोम के सीज़रों या फ़ारस के ख़ुसरुओं ने शत्रु को संकट की स्थिति में देखा तो उसने समझौते की खुली अवहेलना करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। यहां तक कि ख़ुद नौशेरवां और जस्टिनियन, जो रोमन और ईरानी सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, वे भी इस बुराई की सूची में प्रमुखता से शामिल हैं। जब नौशेरवां को अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए शांति की ज़रूरत थी, तो उसने जस्टिनियन की शांति की इच्छा को तुरंत स्वीकार कर लिया और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब उसने देखा कि इटली में सेलिसरियस की सफलताओं के कारण रोम की शक्ति बढ़ रही है, तो उसने हैरा से ग़स्सान पर हमला कर दिया और फिर ख़ुद हैरा की सहायता के लिए खड़ा हो गया, जिससे रोम भी अपने सहयोगी ग़स्सान की मदद करने के लिए मजबूर हो गया। (Gibbon, Roman Empire, vol. 5, chapter XLV)
दूसरी ओर, 571 ई. में इल्खान अत्राक ने जब नौशेरवान से नाराज होकर जस्टिनियन के साथ सहयोगी बनने की इच्छा की, तो उसने भी ईरानी साम्राज्य को नीचा दिखाने के लिए इस अवसर को भुनाते हुए शांति समझौते को तोड़ कर 572 ई. में नौशेरवां के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया। (Sykes vol. 1, page 49)
युद्ध में बर्बरता
प्राचीन काल से दुनिया में योद्धाओं के अधिकारों और दायित्वों की एक बहुत ही प्रारंभिक अवधारणा मौजूद थी। प्राचीन यूनान के विधिवेत्ताओं ने यह नियम बना दिया था कि युद्ध में मारे गए लोगों को दफ़ना दिया जाए, जीते हुए शहरों के धार्मिकस्थलों में शरण लेने वालों को नहीं मारा जाए और धार्मिक गतिविधियों में लगे लोगों के साथ कोई हिंसा नहीं की जाए। (Grote, History of Greece) लेकिन सबसे पहले, ये नियम अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयों के लिए नहीं थे, बल्कि विधिवेत्ताओं ने इन्हें स्वयं अपने गृहयुद्धों के लिए तैयार किया था। दूसरे यह कि व्यावहारिक अर्थों में, राज्यों ने कभी भी इन्हें क़ानून के रूप में स्वीकार या उनका पालन नहीं किया। रोमन साम्राज्य ने विशिष्ट रूप से ग़ैर-रोमन साम्राज्यों के क़ानूनी अस्तित्व को मान्यता नहीं दी और उनसे निपटने में किसी भी दायित्व या अधिकार की अवधारणा की पूरी तरह से अवहेलना की। यही हाल ईरान का था, उनके अनुसार, ग़ैर-ईरानी राष्ट्र बर्बर थे और अनिवार्य रूप से ईरानी साम्राज्य के विद्रोही थे। इसलिए उनसे लड़ने में वे किसी नैतिक दायित्व को महसूस नहीं करते थे।
रोम और ईरान की सैन्य व्यवस्था भी इस प्रकार की थी कि उसमें नैतिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा सकता था। सैन्य प्रशिक्षण, युद्ध के ढंग की शिक्षा तथा सैनिक अनुशासन बनाये रखने का कोई प्रावधान नहीं था। युद्ध के अवसर पर, सामान्य लड़ाके निवासियों की भीड़ केवल ख़ून के खेल में भाग लेने के जुनून में इकट्ठा हो जाती थी, कि पड़ोसी देशों को लूटें, विरोधियों को बर्बाद कर दें और उनकी हिंसा करें। युद्ध के प्रति उनका आकर्षण, धन सम्पत्ति की लूट के अलावा शत्रु राष्ट्र की सुन्दर लड़कियों को दासियाँ बनाकर अपनी वासना पूरी करने के लिए भी था। उनके सेनापतियों के सामने भी युद्ध का कोई नैतिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि वे केवल शत्रुओं को मारने और नष्ट करने के लिए ही तलवार उठाया करते थे। यही कारण है कि जब उनकी सेनाएँ किसी देश में आगे बढ़ती थीं तो बच्चे, बूढ़े, औरतें, जानवर, पेड़, धर्मस्थल, कुछ भी उनके हाथ से सुरक्षित नहीं बचता था। जो लूटा जा सकता था वह लूट लिया जाता और जो नहीं लूटा जा सकता उसे जला दिया जाता।
रोम के साथ अफ्रीका के वैंडल्स और यूरोप के गल्स का हमेशा युद्ध रहता था। इतिहास उनके साथ किए गए बर्बर व्यवहारों से भरा पड़ा है। सीज़र जस्टिनियन के समय में जब नडाल पर हमला किया गया, तो उनके पूरे समुदाय का सफ़ाया कर दिया गया। युद्ध से पहले, उस समुदाय में 1,60,000 योद्धा पुरुष थे, और उनके अलावा बड़ी संख्या में स्त्रियाँ, बच्चे और दास भी मौजूद थे। लेकिन जब रोमन विजेताओं ने उन पर नियंत्रण पा लिया, तो उन में से एक व्यक्ति को भी उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। गिब्बन कहता है कि पूरा देश ऐसा तबाह कर दिया गया था कि एक अजनबी पर्यटक उस वीराने में सारा-सारा दिन घूमता था और उसे कहीं कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता था। प्रोकोपियस ने जब पहली बार उस भूमि पर पांव रखा था, तो वह उसकी आबादी, समृद्धि, व्यापार और कृषि का विकास देखकर चकित रह गया था। फिर 20 वर्षों से भी कम समय में, वह सारी चहल-पहल वीरानी में बदल गई और पचास लाख की महान आबादी जस्टिनियन के आक्रमण और उत्पीड़न के कारण नष्ट हो कर रह गई। (गिब्बन, वॉल्यूम 5, अध्याय XLIII)
यूरोप में गल्स के साथ भी उसी बर्बरता का व्यवहार किया गया था। यहां तक कि जब उनका राजा टोटिला युद्ध के मैदान से घायल होकर भागा और एक दूर स्थान पर जाकर मर गया, तो रोमन सैनिक उसकी तलाश में निकल पड़े। उसकी लाश से कपड़े उतार लिए और सीज़र जस्टिनियन को उपहार के रूप में ताज के साथ उसके ख़ून में सने कपड़े भेज दिए। (गिब्बन, वॉल्यूम 5, अध्याय XLIII)
जब टाइटस रोमन ने 70 ईस्वी में यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तो लंबी सुंदर लड़कियां विजेता के लिए चुन ली गईं। 17 वर्ष से अधिक आयु के हज़ारों पुरुषों को पकड़ लिया गया और मिस्र की खानों में काम करने के लिए भेज दिया गया, कई हज़ार पुरुषों को गिरफ़्तार कर लिया गया और साम्राज्य के विभिन्न शहरों में भेज दिया गया, ताकि एम्फी थिएटरों और क्लोसिमों में उन को जंगली जानवरों द्वारा फड़वाने और तलवारबाज़ों से कटवाने या ख़ुद आपस में एक दूसरे को काटने के काम में लाया जा सके। युद्ध के दौरान, 97,000 लोगों को बंदी बना लिया गया, जिनमें से 11,000 केवल इसलिए मर गए कि उनके पहरेदारों ने उन्हें भोजन नहीं दिया। उनके अलावा युद्ध और नरसंहार में मरने वालों की कुल संख्या 133749 बताई जाती है। (फेरार, अर्ली डेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, पीपी. 488-89)
रोम और ईरान के आपसी युद्धों में भी इसी प्रकार के बर्बर कृत्य किये जाते थे। जब शापुर जुलकताफ़ अल-जज़ायर की ओर बढ़ा और उग्र प्रतिरोध के बाद अमेदाह (वर्तमान दियारबाकिर) पर विजय प्राप्त की, तो क्रोधित विजेता ने शहर में प्रवेश करते ही नरसंहार का आदेश दे दिया और उसे ऐसा बर्बाद कर दिया कि वह फिर पनप नहीं सका। 540 ईस्वी में नौशेरवां ने जब सीरिया पर चढ़ाई की, तो उसकी राजधानी एंटिओक और फामिया आदि दुसरे शहरों को लूट लिया, उन्हें जला दिया, 2,92,000 सीरियाई लोगों को पकड़ कर ईरान भेज दिया। बहुत सी खूबसूरत लड़कियों का चयन किया और उन्हें इल्खान अत्राक के पास भेज दिया ताकि वे उसकी नाराज़ी दूर हो और वह जस्टिनियन के साथ गठबंधन छोड़ दे। 576 ईस्वी में उसने अर्मेनिया पर आक्रमण किया, और जब थियोडोसियस पोलिस को जीतने में विफल रहा, तो वह कप्पादोसिया में घुस गया और जो कुछ भी उसके सामने आया उसे नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि मेलटीन को भी जला कर राख कर दिया। सीरिया, फ़िलिस्तीन और एशिया। इसके अलावा, दमिश्क, एंटिओक और अलेप्पो जैसे शहरों का भाग्य बहुत अलग नहीं था (ये सभी विवरण गिब्बन, साइक्स और फोर्ड की किताबों से प्राप्त किये हुए हैं)।
ये बर्बर आन्दोलन कभी-कभी घोर छल और कायरतापूर्ण षडयंत्रों के रूप में भी प्रकट होते थे। अत: अर्दशिर की घटना सर्वविदित है कि जब वह ख़ुसरो अर्मनिस्तान को सैन्य बल से पराजित नहीं कर सका तो उसने अपनी सेना के एक अधिकारी को गुप्त रूप से भेज कर उसे मरवा दिया। रोम और ईरान के इतिहास में ऐसी घटनाएं अनोखी नहीं हैं। (साइक्स, खंड 1, पीपी :427-28)
युद्धबंदियों की स्थिति
सबसे बढ़कर दुर्व्यवहार जिस समूह के साथ होता था, वह युद्धबंदियों का समूह था। प्राचीन रोमन और यूनानी अपने अलावा अन्य राष्ट्रों को जंगली और बर्बर मानते थे। उनके क़ानून में उस अभागे प्राणी के लिए हत्या या ग़ुलामी के अलावा कोई तीसरा विकल्प मौजूद नहीं था। अरस्तू जैसा नैतिक शिक्षक स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रकृति ने बर्बर जाति की रचना केवल ग़ुलामी के लिए की है (राजनीति) एक अन्य बिंदु पर, वह धन प्राप्त करने के वैध और सम्मानजनक तरीक़ों को गिनाते हुए कहता है कि उन जातियों को ग़ुलाम बनाने के लिए युद्ध करना भी उन तरीक़ों में से एक है, जिन्हें प्रकृति ने इसी उद्देश्य के लिए पैदा किया है। (वही, किताब 1, अध्याय VIII)
एक ओर इन मान्यताओं ने रोमनों के मन में अन्य जातियों के जीवन और संपत्ति का अवमूल्यन कर दिया था, दूसरी ओर रोमन समाज का पालन-पोषण ऐसे राक्षसी वातावरण में हुआ कि लोग उनके खेलों में भयानक दृश्यों को देखकर खुश होते थे। वे उन दृश्यों में बनावट के बजाय वास्तविकता को देखना पसंद करते थे। अगर किसी घर को जलता हुआ दिखाना था, तो वे चाहते थे कि एक असली घर को जला दिया जाए। इसी तरह, अगर किसी आदमी को ज़िंदा जलाया जाना या एक अपराधी को शेरों द्वारा टुकड़े-टुकड़े करना दिखाया जाना होता, तो दर्शकों की संतुष्टि इसके बिना नहीं होती कि एक आदमी को वास्तव में ज़िंदा जला दिया जाए और दूसरे आदमी को वास्तव में शेरों के पिंजरे में छोड़ दिया जाए। इन कामों के लिए उन्हें हमेशा ऐसे आदमियों की ज़रूरत रहती थी जो इन बर्बर खेलों के लिए इस्तेमाल किए जा सकें। ज़ाहिर है, कि रोम के मुक्त नागरिक इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसलिए, अन्य देशों से लड़ाई में पकड़े गए क़ैदियों को इस ख़ूनी मनोरंजन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कभी-कभी ये खेल इतने बड़े पैमाने पर होते थे कि एक साथ कई हज़ार लोगों को तलवार के हवाले कर दिया जाता था। मानव जाति के प्रिय कहे जाने वाले टिटोस ने एक बार 50,000 जंगली जानवरों को पकड़वा लिया और उनके साथ एक बाड़े में कई हज़ार यहूदी क़ैदियों को छोड़ दिया था। ट्रोजन के खेलों में ग्यारह हज़ार जानवर और दस हज़ार आदमी एक साथ लड़ाए जाते थे। क्लॉडियस ने एक बार युद्ध के खेल में 19,000 लोगों को तलवारें देकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़वा दिया। सीजर ऑगस्टस ने अपनी वसीयत के साथ जो लेख जोड़ा था, उसमें लिखा है कि मैंने 8 हज़ार तलवारबाज़ों और 3510 जानवरों के खेल देखे हैं। ये सारे मनोरंजन युद्धबंदियों द्वारा ही संचालित किए जाते थे।
इसके अलावा, युद्धबंदियों का अन्य उपयोग स्वतन्त्र व्यक्तियों की ग़ुलामी करना था। उनका पद समाज में सबसे नीचे था। उनका कोई परिभाषित अधिकार नहीं था। उनकी जान की कोई क़ीमत नहीं थी। उनके जीवन का उद्देश्य अपने आक़ाओं की हर इच्छा को पूरा करने के सिवा और कुछ नहीं था। फेरर के अनुसार, “वे बचपन में अपमान के, युवावस्था में परिश्रम के, और वृद्धावस्था में बेरहमी और उपेक्षा के पात्र थे। (फेरर, पी-2) रोमन क़ानून में दासों के लिए इतने सख़्त नियम थे कि अगर कोई ग़ुलाम अपने स्वामी के ख़िलाफ़ विद्रोह करता तो, उसे और कभी-कभी उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता। (रेव, कट. कॉन्सटेंटाइन द ग्रेट, पी-57) 611 में जब हर्कुलिस द्वारा सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उसकी पत्नी युडोक्सिया की मृत्यु हो गई और उसके अंतिम संस्कार का जुलूस क़ब्रिस्तान जा रहा था। जुलूस के साथ साथ जाते समय एक ग़ुलाम लड़की ने ग़लती से जमीन पर थूक दिया। उसे इस अपराध के लिए तुरंत गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके सज़ा-ए मौत का आदेश दे दिया गया। (बीजान्टिन साम्राज्य, पी-99)।
फेरर का कहना है कि जब रोम की विजय का दायरा बढ़ा, तो बड़ी संख्या में युद्धबंदी राज्य में आने लगे और एक समय में उनकी कुल संख्या 6 करोड़ तक पहुंच गई। (फेरर, पी-2)
ईरान में भी युद्ध बंदियों के हालात रोम की तरह, ही थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। साधारण क़ैदी तो क्या जब सीज़र वेलेरियन शापुर प्रथम द्वारा क़ैद किया गया था, तो उसे भी ज़ंजीरों में जकड़ कर शहर में गश्त कराया गया था, जीवन भर उससे ग़ुलामों की तरह सेवा ली गई, और उसकी मृत्यु के बाद, उसकी त्वचा को खींचकर उसमें भुस भरवा दिया गया।(साइक्स, वॉल्यूम-1) शापुर जुलअकताफ़ की घटना प्रसिद्ध है कि बहरीन और अल-हिसाअ में युद्ध के अरब क़ैदियों से बदला लेने के लिए, उसने उनके कंधों में छेद करने और उनके अंदर रस्सियाँ डालकर उन सभी को एक साथ बाँधने का आदेश दिया। (साइक्स, वॉल्यूम-1)
रक्तपात की ये दास्तानें और भी भयानक हो जाती हैं, जब हम सुनते हैं कि मानव जाति पर यह अत्याचार किसी उच्च उद्देश्य के लिए नहीं किए गए थे, बल्कि केवल प्रसिद्धि और महिमा की अभिव्यक्ति के लिए किए जा रहे थे। कभी-कभी ऐसा भी होता कि राजाओं के बहुत ही तुच्छ स्वार्थों के लिए हज़ारों-लाखों लोगों के जान की भेंट चढ़ा दी जाती। पैग़म्बर (सल्ल.) के समय की एक घटना है कि ख़ुसरो परवेज़ ने नुअमान बिन मुंजिर की बेटी की सुन्दरता की प्रशंसा सुनी तो उन्हें अपनी बेटी को लेकर शाही हरम में आने का आदेश दे दिया। नुअमान का अरब गौरव इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने सपाट रूप से मना कर दिया। इस पर ख़ुसरो ने फरमान जारी किया कि हैरा के राज्य को ज़ब्त कर लिया जाए और नुअमान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। नुअमान ने अपने परिवार को बनी शैबन के संरक्षण में दिया और क्षमा माँगने के लिए ख़ुद ख़ुसरो के दरबार में पहुंचे। लेकिन ख़ुसरो ने उसे मार डाला और 40,000 की एक मज़बूत सेना को बनी शैबान से नुअमान बिन मुंज़िर के परिवार को छीन लाने के लिए भेजा। ज़ुक़ार के स्थान पर, इस सेना का अरबों के साथ ख़ूनी युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों के हज़ारों पुरुष मारे गए और मानव रक्त की नदियाँ केवल इस बात के लिए बहाई गईं कि एक राजा अपने कक्ष में एक सुंदर महिला को देखना चाहता था।
इस संक्षिप्त ऐतिहासिक वृत्तांत से स्पष्ट है कि उस युग में युद्ध की नैतिक सीमाएँ, योद्धाओं के अधिकार और दायित्व, शत्रुता में आत्म-संयम और युद्ध में दया और क्रोध के संयोजन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जहाँ तक युद्ध का संबंध है, तो सबसे सभ्य राष्ट्र भी बर्बरता की आदिम अवस्था में थे। उस युग में युद्ध का अर्थ हिंसा, हत्या, रक्तपात और उत्पात के सिवा कुछ भी नहीं था। जो शक्तिशाली था, वह अपनी इच्छा और ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रूरता, दमन और अत्याचार की किसी भी सीमा तक जा सकता था। युद्ध शब्द का उल्लेख करते ही, दिमाग़ किसी ऐसी चीज़ की ओर चला जाता था जिसमें मानव जीवन लेने और उसकी आबादी को लूटने के हर तरीक़े शामिल थे। सदियों के बर्बरतापूर्ण कृत्यों का युद्ध से इतना घनिष्ठ संबंध था कि मनुष्य ऐसे युद्ध की शायद ही कल्पना कर सकता था जिसमें कोई लूट, नरसंहार, आगज़नी और विनाश न हो, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, घायल और बीमार लोग न मारे जाते हों, जिसमें अन्य धर्मों और राष्ट्रों की इबादतगाहों और स्मारकों को अपवित्र और नष्ट नहीं किया जाता हो, और लड़ाई नैतिक सीमाओं के पालन के साथ की जाती हो।
(3) इस्लामी सुधार
यह वह दुनिया थी जिसमें इस्लाम ने सुधार का क़दम बढ़ाया। उसने युद्ध की वास्तविकता को बदल दिया और एक बिल्कुल नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिससे दुनिया तब तक अपरिचित थी। उसका सिद्धांत है कि युद्ध और लड़ाई मूल रूप से एक गुनाह है जिससे हर इंसान को बचना चाहिए, लेकिन जब दुनिया में इससे बड़ा गुनाह, यानी अत्याचार, विद्रोह, उपद्रव और अव्यवस्था फैल गई हो और उपद्रवी लोगों ने अल्लाह की सृष्टि की शांति भंग कर दी हो और सुख-सुविधा को संकट में डाल कर उनका जीना दूभर कर दिया हो, तो युद्ध न केवल अनुज्ञेय हो जाता है, अपितु अल्लाह की सृष्टि को हानि से बचाने के लिए ही युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है।
युद्ध की इस्लामी अवधारणा
इस सिद्धांत के अनुसार, चूँकि युद्ध का वास्तविक उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को मारना और नुक़सान पहुँचाना नहीं है, बल्कि केवल उसकी बुराई को दूर करना है, इस्लाम यह सिद्धांत देता है कि युद्ध में केवल उतना ही बल प्रयोग किया जाना चाहिए जितना कि बुराई को दूर करने के लिए अपरिहार्य हो और इस बल का प्रयोग केवल उन्हीं वर्गों के विरुद्ध किया जाना चाहिए जो वास्तव में लड़ रहे हों या हद से हद यह कि जिनसे बुराई की आशंका हो। मानव जाति के अन्य सभी वर्गों को युद्ध के प्रभाव से सुरक्षित रहना चाहिए और दुश्मन की ऐसी चीज़ों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जिसका उसकी युद्धक शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। युद्ध की यह अवधारणा उन धारणाओं से अलग थी जो आम तौर पर ग़ैर-मुस्लिम दिमागों में मौजूद थीं, इसलिए इस्लाम ने सभी मौजूदा शब्दों और शर्तों को त्याग दिया और एक अलग शब्द “जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह” की रचना की, जो अपने अर्थ में अधिक सटीक है। यह अवधारणा शाब्दिक रूप से, इसे बर्बर युद्ध की अवधारणाओं से पूरी तरह अलग करती है। शब्दकोश के अनुसार, जिहाद का अर्थ है “किसी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना। इस शब्द में ‘हर्ब’ की तरह क्रोध और घृणा का अर्थ नहीं है, न ही ‘रौअ’ की तरह भय और आतंक का, और न ‘शर’ की तरह बुराई और शरारत का, न ‘निताह’ की तरह हैवानियत और पशुता का, न ही ‘करीहा’ की तरह दुख और कष्ट का। इसके विपरीत, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुजाहिद (जिहाद करने वाले) का मुख्य उद्देश्य नुक़सान को दूर करना है और इसके लिए वह उतना ही प्रयास करता है जितना नुक़सान को ख़त्म करने के लिए आवश्यक है। इस अर्थ के लिए केवल “प्रयास” शब्द का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह शब्द “प्रयास” अच्छाई के लिए भी हो सकता है और बुराई के लिए भी। इसलिए, ‘अल्लाह की राह’ की शर्त लगा दी गई, ताकि अपनी किसी इच्छा, किसी देश को विजय करने, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने, या धन संपत्ति या सत्ता या शक्ति या प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास करने को इसमें शामिल नहीं किया जा सके और केवल उसी प्रयास को मान्यता दी जाए जो विशुद्ध रूप से अल्लाह के लिए हो। जिसमें निज स्वार्थ की कोई आशंका तक न हो और अपनी शक्ति और क्षमता को ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में ख़र्च किया जाए, जो अल्लाह को पसंद हो।
इस शुद्ध अवधारणा के तहत, इस्लाम ने युद्ध का एक पूरा कोड तैयार किया, जिसमें युद्ध के तरीक़े, उसकी नैतिक सीमाएं, लड़ाकों के अधिकार और दायित्व, लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच का अंतर, और सभी के अधिकार, संधि वाले राष्ट्रों के अधिकार शामिल हैं। जिसमें राजदूतों और युद्धबंदियों के अधिकारों, विजित राष्ट्रों के अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया। सभी के लिए सामान्य नियम और आवश्यक आदेश निर्धारित किए गए, और इसके साथ ही, इस्लाम के आवाहक हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) और उनके सच्चे ख़लीफ़ाओं ने भी युद्ध के क़ानूनों और सामान्य नियमों को लागू करने के लिए उदाहरणों का एक बड़ा संग्रह छोड़ा।
युद्ध के उद्देश्य में सुधार
क़ानून बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि कागजों पर क़ानूनों की संहिता आ जाए, बल्कि वास्तविक उद्देश्य व्यावहारिक त्रुटियों को ठीक करना और युद्ध के बर्बर तरीक़ों को ख़त्म करके उस की जगह इस सभ्य क़ानून को प्रचलित कराना था। इसके लिए सबसे पहले उस ग़लत अवधारणा को दिलों से मिटाना ज़रूरी था, जो सदियों से जमी हुई थी। लोगों की बुद्धि इसे समझने में असमर्थ थी कि जब धन-संपदा के लिए युद्ध न किया जाए, देश-भूमि के लिए न किया जाए, यश-प्रतिष्ठा के लिए न किया जाए, साम्प्रदायिकता और द्वेष के लिए न किया जाए, तो फिर युद्ध का उद्देश्य क्या हो सकता है। ऐसे युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसका स्वार्थ और निज लाभ से कोई लेना-देना न हो। इसलिए, इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) ने सबसे पहला काम यही किया कि अल्लाह की राह में जिहाद का अर्थ और उसकी सीमाओं को, जो उसे अल-ताग़ूत (असत्य) के मार्ग में जिहाद से पूरी तरह अलग करती है, स्पष्ट किया और अलग-अलग तरीक़ों से इस पवित्र अवधारणा को समझाया। इसके बारे में कई हदीसें हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दर्ज हैं।
अबू मूसा अशअरी से वर्णित है कि:
“एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के पास आया और बोला, कोई व्यक्ति लूट का माल हासिल करने के लिए युद्ध करता है, कोई ख्यति के लिए युद्ध करता है, कोई अपनी बहादुरी दिखाने के लिए युद्ध करता है, इनमें से किसका युद्ध ख़ुदा की राह में है? अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने जवाब दिया कि ख़ुदा की राह में युद्ध तो केवल उस व्यक्ति का है जो केवल अल्लाह का बोल ऊंचा करने के लिए युद्ध करता है।”
यही अबू मूसा बयान करते हैं:
“एक आदमी नबी (सल्ल.) के पास आया और बोला, ऐ अल्लाह के रसूल! “अल्लाह की राह में लड़ना क्या है?
आप (सल्ल.) ने अपना सिर उठाया और जवाब दिया कि जो व्यक्ति अल्लाह का बोल ऊंचा करने के लिए युद्ध करता है। वह अल्लाह के रास्ते में युद्ध करता है।”
उबादा बिन सामित बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा “जो व्यक्ति अल्लाह के मार्ग में लड़ने के लिए गया और केवल ऊंट बाँधने की एक रस्सी की नीयत कर ली, तो उसे केवल वह रस्सी ही मिलेगी और सवाब कोई नहीं मिलेगा।”
मुआज़ बिन जबल के हवाले से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा:
“युद्ध दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति जो केवल अल्लाह की ख़ुशी के लिए लड़ा और उसमें सेनापति की आज्ञा का पालन किया, उसमें अपना अच्छे से अच्छा माल ख़र्च किया और बिगाड़ से बचा रहा, तो उसका सोना-जागना सब इनाम के योग्य है, और जो कोई सांसारिक दिखावे और शोहरत के लिए लड़े और युद्ध में सेनापति की अवज्ञा करे और ज़मीन में फ़साद फैलाए तो वह बराबर पर भी नहीं छूटेगा। (यानी उल्टा उस को सज़ा भुगतनी पड़ेगी)”
हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार नबी (सल्ल.) ने कहा:
क़ियामत के दिन सबसे पहले तीन तरह के लोगों का न्याय किया जाएगा। पहले वह व्यक्ति लाया जाएगा जो लड़कर शहीद हुआ था, अल्लाह उसे अपने उपकार गिनाएगा और जब वह उन्हें स्वीकार कर लेगा, तो अल्लाह पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया? वह कहेगा कि मैं ने तेरे लिए युद्ध किया, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। इस पर अल्लाह कहेगा, तूने झूठ कहा, तू तो इसलिए लड़ा कि लोग तुझे बहादुर कहें। तो तेरा यह लक्ष्य पूरा हो गया है। तब अल्लाह उसके लिए दण्ड का आदेश देगा और उसे औंधे मुँह घसीट कर नरक में डाल दिया जाएगा।
अब्दुल्लाह बिन मसूद से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा:
“क़ियामत के दिन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़कर आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मेरी हत्या की थी। अल्लाह पूछेगा कि तूने इसकी हत्या क्यों की थी। वह कहेगा कि मैंने इसकी हत्या इसलिए की कि सम्मान तेरे लिए हो। फिर एक दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मेरी हत्या की थी। अल्लाह पूछेगा कि तूने इसकी हत्या क्यों की थी। वह कहेगा कि मैंने इसकी हत्या इसलिए की कि सम्मान उक्त व्यक्ति के लिए हो। इस पर अल्लाह उससे कहेगा कि कि सम्मान उसके लिए तो नहीं था। फिर वह उस अपराध में पकड़ा जाएगा।”
यह शिक्षा युद्ध को सभी सांसारिक उद्देश्यों से मुक्त कर देती है। प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा, सम्मान और अधिकार की इच्छा, धन का लालच और लूट के माल का लोभ, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय शत्रुता का बदला, आदि ऐसा कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं है जिसके लिए युद्ध की अनुमति हो। इन चीज़ों के अलग हो जाने के बाद, युद्ध केवल एक नीरस और बेस्वाद नैतिक और धार्मिक दायित्व रह जाता है, जिसके ख़तरों में शामिल होने की इच्छा कोई भी नहीं कर सकता है, और अगर दूसरों द्वारा फ़ित्ना की शुरुआत की जाती है, तो भी वह लड़ाई के लिए तलवार केवल तब उठा सकता है, जब स्थिति को सुधारने और नुक़सान को दूर करने के लिए तलवार के सिवा और कोई साधन नहीं बचा हो। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ख़ुद कह दिया है कि:
“दुश्मन से भिड़ने की इच्छा न करो और अल्लाह से सलामती की दुआ किया करो, लेकिन जब दुश्मन से सामना हो जाए तो फिर जम कर लड़ो, और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है।”
युद्ध की पद्धति में सुधार
लक्ष्य में सुधार के साथ-साथ इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) ने लक्ष्य प्राप्त करने के तरीक़े में भी सुधार किया और इस्लामपूर्व अरब की लड़ाइयों में की जाने वाली सभी बर्बर कार्रवाइयों को धीरे-धीरे बंद कर दिया। इससे जुड़े कई निषेध हैं जिनमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह से बर्बर कृत्यों की मनाही है।
ग़ैर-लड़ाकों का सम्मान
इस संबंध में पहली बात यह है कि युद्धरतों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक योद्धा या लड़ाके और दूसरा ग़ैर-लड़ाके। योद्धा वे हैं, जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से युद्ध में भाग लेने की क्षमता रखते हैं, यानी युवा पुरुष। और ग़ैर-लड़ाके वे हैं जो सामान्य रूप से लड़ाई में भाग नहीं ले सकते हैं, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, घायल, अंधे, विकलांग, पागल, पर्यटक, भिक्षु, साधु, और जो लोग मंदिरों और मठों की सेवा में लगे रहते हैं और ऐसे अन्य हानिरहित लोग। इस्लाम ने युद्ध के दौरान प्रथम श्रेणी के लोगों की हत्या की अनुमति दी है और द्वितीय श्रेणी के लोगों की हत्या को हराम (वर्जित) ठहराया है।
एक बार जंग के मैदान में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने एक औरत की लाश देखी। नाराज़ हो कर कहने लगे कि यह तो लड़ने वालों में से नहीं है। तब सेना के कमांडर ख़ालिद को यह आदेश भेजा, “महिला और आम मज़दूर की हत्या न की जाए।”
एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया:
“न किसी बूढ़े दुर्बल की हत्या की जाए, न किसी छोटे बच्चे की और न किसी स्त्री की, विजयधन की चोरी न की जाए, युद्ध में जो कुछ मिले उसे एक जगह इकट्ठा करो, उपकार और भलाई करो, क्योंकि अल्लाह भलाई करने वालों को पसन्द करता है।”
मक्का की विजय के अवसर पर, पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) ने पहले से निर्देश दे दिया था कि किसी घायल व्यक्ति पर हमला न करें, जो अपनी जान बचाकर भागे उसका पीछा न करें, और जो कोई भी अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए, उसे शांति प्रदान करें। (फ़त्हुल- बलदान, पृष्ठ 47)
इब्न अब्बास द्वारा वर्णन किया गया है कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) कहीं सेना भेजते थे, तो उन्हें निर्देश दे देते कि “मठवासी तपस्वियों और मठों की सेवा में लगे लोगों की हत्या न करना।”
इन विभिन्न छोटे-छोटे आदेशों से, इस्लामी न्यायविदों ने यह नियम निकाला है कि वे सभी लोग जो लड़ने में अक्षम हैं या अपनी आदत के कारण अक्षम की श्रेणी में हैं, उन्हें युद्ध से छूट प्राप्त है। लेकिन उनका अपवाद पूर्ण नहीं है बल्कि इस शर्त के साथ कि वे वास्तव में युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। अगर उनमें से कोई वास्तव में युद्ध में भाग लेता है, उदाहरण के लिए, बीमार बिस्तर पर लेटे-लेटे सेना को रणनीति बता रहा हो, या महिला जासूसी कर रही हो, या बच्चा गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, या धर्म से जुड़ा कोई व्यक्ति शत्रु राष्ट्र को युद्ध के लिए उकसा रहा हो, तो उसे मारने की अनुमति होगी। क्योंकि उन्होंने स्वयं को लड़ाकों में शामिल करके ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों से ख़ुद को वंचित कर लिया है।
लड़ाकों के अधिकार
ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों का वर्णन करने के बाद यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर तलवार उठाने की अनुमति है, तो वह अनुमति भी असीमित नहीं है, बल्कि उसकी कुछ सीमाएँ हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। इन सीमाओं को एक-एक करके विस्तार से समझाया गया है।
अप्रत्याशित हमले का निषेध
अरबवासी रात में अचानक हमला बोलते थे, ख़ासकर रात में जब लोग बेख़बर सो रहे होते थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस आदत को बंद कर दिया और यह नियम स्थापित किया कि सुबह होने से पहले किसी भी दुश्मन पर हमला नहीं किया जाए। अनस बिन मालिक ख़ैबर की लड़ाई का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि “जब पैग़म्बर (सल्ल.) रात में किसी दुश्मन राष्ट्र में पहुंच जाते, तो वे सुबह तक हमला नहीं करते।”
आग में जलाने का निषेध
अरब और ग़ैर-अरबी बदला लेने के लिए दुश्मन को ज़िंदा जला देते थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने इस बर्बर कृत पर भी रोक लगा दी। उन्होंने कहा, “आग की सज़ा आग पैदा करने वाले के सिवा किसी के लिए नहीं है।”
बंधे हुए क़ैदी को मारने का निषेध
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने दुश्मन को बांधकर मारने और पीड़ा देकर मारने से भी मना किया है। उबैद बिन याला ने बताया कि हम अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद के साथ युद्ध में गए थे, एक मौक़े पर उनके सैनिक चार दुश्मनों को पकड़ कर लाए और उन्हें बांधकर मारने का आदेश दिया। जब इस बात का ज़िक्र हज़रत अयूब अंसारी से किया गया तो उन्होंने कहा:
“मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि उन्होंने बांधकर मारने से मना किया है। अल्लाह की क़सम, अगर मुर्ग़ी भी होती तो मैं उसे इस तरह बांधकर नहीं मारता। इस की ख़बर जब अब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद को पहुंची, तो उन्होंने उन चारों को मुक्त कर दिया (और अपनी ग़लती के लिए प्रायश्चित किया।)
लूट-मार का निषेध
ख़ैबर युद्ध में समझौता हो जाने के बाद जब इस्लामी सेना की कुछ नई भर्तियां बेक़ाबू हो गईं और उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी, तो यहूदियों का नेता, अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के पास आया और पैग़म्बर (सल्ल.) को कठोर स्वर में संबोधित किया और कहा, “ऐ मुहम्मद! क्या तुमको शोभा देता है कि हमारे जानवरों को मारो, हमारे फल खाओ और हमारी महिलाओं को परेशान करो? इस पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने तुरंत इब्ने औफ़ को सैनिकों में इकट्ठा करने और शांति का प्रचार करने का आदेश दिया। जब सेना के सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) खड़े हो गए और कहा:
“क्या तुम में से कोई घमंड के सिंहासन पर बैठा है, यह सोचता है कि अल्लाह ने क़ुरआन में हराम की गई चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ को हराम नहीं किया है? अल्लाह की क़सम, मैं तुम्हें जो उपदेश देता हूं और मैं जो आदेश देता हूं वे भी क़ुरआन की तरह हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अहले किताब के घरों में बिना अनुमति प्रवेश करना, उनकी स्त्रियों को पीटना और उनके फल खाना जायज़ नहीं किया है, हालांकि उन्होंने तुम्हें वह सब दे दिया है, जो उनपर अनिवार्य था।”
एक बार जिहाद के दौरान सेना के लोगों ने कुछ बकरियां लूट लीं और उनका मांस पकाकर खाना चाहते थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को इस के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने आकर कड़ाहों को पलट दिया, और कहा, लूटा-खसोट का माल मुर्दार से बेहतर नहीं है।”
अब्दुल्ला बिन यज़ीद से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने लूटे हुए धन को हराम क़रार दिया है।
अगर रास्ते में दूध देने वाले जानवर मिल जाएं, तो उनके दूध पीने की अनुमति नहीं है। जब तक उनके मालिकों से अनुमति नहीं ले ली जाए। सख़्त ज़रूरत की हालत में केवल इतनी इजाज़त है कि तीन बार ज़ोर से पुकारा जाए ताकि अगर कोई मालिक हो तो आ जाए और अगर कोई न आए तो उसका दूध पिया जा सकता है।
विनाश का निषेध
सेना के आगे बढ़ने के दौरान फ़सलों का विनाश, खेतों का विनाश, नरसंहार और बस्तियों में आगज़नी युद्ध के नियमों में शामिल है, लेकिन इस्लाम इसे उद्दंडता बताता है और इसे नाजायज़ बताते हुए ऐसा करने वालों की कड़ी निंदा करता है। क़ुरआन में इसका उल्लेख है:
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ○ (البقرہ :۲۰۵)
“जब वह शासक बन जाता है, तो वह भूमि में अशांति फैलाने और फ़सलों और पीढ़ियों को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह बिगाड़ को पसंद नहीं करता है।” (अल-बक़रा : 205)
हज़रत अबू बक्र जब सीरिया और इराक़ में सेना भेज रहे थे तो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों में से एक यह भी था कि बस्तियों को उजाड़ मत करना और फ़सलों को बर्बाद मत करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर युद्ध की ज़रूरत हो तो पेड़ों को काटकर और जलाकर मैदान साफ़ कर देने की अनुमति है। जैसा कि बनी नज़ीर की घेराबंदी में किया गया था। लेकिन केवल विनाश के इरादे से ऐसा करना मना है।
विरोधियों ने बनी नज़ीर की घटना को इस आरोप के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है कि इस्लाम युद्ध में लूटपाट और दुश्मन की फ़स्लों को तबाह करने की अनुमति देता है। लेकिन घटनाओं के शोध से यह साबित होता है कि बनू नज़ीर के खजूर के पेड़ों को काटना और जलाना सामरिक आव्श्यकता पर आधारित था, उसका उद्देश्य दुश्मन को नुक़सान पहुँचाना या उससे बदला लेना नहीं था। ध्यान देने की बात यह भी है कि जिन पेड़ों को काटा गया था, वे क़ुरआन की व्याख्या के अनुसार एक विशेष प्रकार के खजूर के पेड़ थे, जिन्हें ‘लीना’ कहा जाता है और बनू नज़ीर उस खजूर का इस्तेमाल भोजन के लिए नहीं करते थे।
مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ٥(الحشر:۵)
“तुमने नहीं काटा कोई लीना (खजूर का वृक्ष) और न छोड़ा उसे खड़ा अपने तने पर, परन्तु ये सब अल्लाह के आदेश से हुआ और ताकि वह अपमानित करे पथभ्रष्टों को।” (अल-हश्र :5)
मृतकों के अंगभंग का निषेध
इस्लाम ने दुश्मन के शवों को अपमानित करने और उनके अंगों को क्षत-विक्षत करने को सख़्ती से मना किया है। अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी बयान करते हैं कि:
“अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने लूट के माल और ‘मुसला’ (अंग-विच्छेदन) से मना किया है।”
सेनाओं को भेजते समय पैग़म्बर (सल्ल.) जो निर्देश देते थे, उनमें वे इस बात पर ज़ोर देते थे:
वचन-भंग न करना, विजयधन की चोरी न करना, और ‘मुसला’ (अंग-विच्छेदन) न करना।”
बंदी-हत्या का निषेध
मक्का की विजय के अवसर पर, जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने शहर में प्रवेश किया, तो उन्होंने सेना में घोषणा करा दी कि:
“किसी घायल पर आक्रमण न किया जाए, न किसी भागने वाले का पीछा किया जाए, न किसी क़ैदी का वध किया जाए, और जो अपने घर का द्वार बन्द करले, वह सुरक्षित है।”
हज्जाज बिन यूसुफ़ ने एक बार हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को एक बंदी की हत्या करने का आदेश दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि यह आदेश दिया है कि जो लोग गिरफ़्तार होकर आएं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो या फिरौती लेकर रिहा कर दो।
दूत की हत्या का निषेध
पैग़म्बर (सल्ल.) ने दूतों और संदेशवाहकों की हत्या को भी मना किया है। जब मुसैल्मा क़ज़्ज़ाब का दूत, उबादा बिन हरिस, अपने आपत्तिजनक संदेश के साथ आया, तो पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा:
“अगर दूतों की हत्या निषिद्ध नहीं होती, तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार देता।”
वचनभंग का निषेध
विश्वासघात, वचनभंग और समझौतों को तोड़ने के बारे में कई हदीसें हैं, जिसके आधार पर इस काम को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह ठहराया गया है। अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है कि पैग़म्बर (सल्ल.) ने फ़रमाया:
“जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को मारता है, जिसके राष्ट्र के साथ समझौता हो, तो वह स्वर्ग की सुगंध भी नहीं पा सकेगा, हालांकि उसकी सुगंध 40 साल की दूरी से महसूस की जाती है।” एक अन्य हदीस में वर्णित है कि:
“हर ग़द्दार और समझौता तोड़ने वाले की बेईमानी की घोषणा करने के लिए क़ियामत के दिन एक झंडा होगा जो उसके विश्वासघात के बराबर होगा और याद रखो कि राष्ट्र मुखिया अगर गद्दारी करे तो उस से बड़ा कोई ग़द्दार नहीं है।”
एक बार जब अमीर मुआविया रोम के शहरों पर हमला करने जा रहे थे, हालांकि युद्धविराम की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी। अमीर मुआविया ने अवधि समाप्त होते ही हमला करने का इरादा किया था। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथियों में से एक, अम्र बिन अंबसा, ने अमीर मुआविया से कहा कि युद्धविराम या शांति-काल के दौरान युद्ध की तैयारियां और सेना का सीमाओं पर प्रस्थान भी ग़द्दारी है, मुआविया ने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कहा: मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना है कि:
“जिस किसी के साथ किसी राष्ट्र की संधि हो, उसे उसकी अवधि समाप्त होने तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर उसकी ओर से विश्वासघात की आशंका हो तो समानता को ध्यान में रखते हुए उसे संधि की समाप्ति की सूचना देनी चाहिए।”
अव्यवस्था का निषेध
अरबों की आदत थी कि जब वे युद्ध के लिए निकलते थे तो रास्ते में जो मिलता था उसे परेशान करते थे और जब वे किसी स्थान पर उतरते थे तो पूरे फर्श पर फैल जाते थे, यहाँ तक कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता था। इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) ने आकर इस पर रोक लगा दी। एक बार जब अल्लाह के रसूल जिहाद के लिए जा रहे थे तो आपको शिकायत मिली कि इस्लामपूर्व अरब के युग की तरह सेना में अव्यवस्था हो गई है और लोगों ने रास्तों को संकीर्ण कर दिया है। इस पर, पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) ने उपदेश दिया कि उन लोगों का जिहाद नहीं होगा जो किसी को परेशान करते हैं या राहगीरों को लूटते हैं।
एक अन्य अवसर पर, उन्होंने कहा: “तुम्हारा इस तरह घाटियों में फैल जाना एक शैतानी कार्य है। अबू सअलबा ख़शनी बयान करते हैं कि उसके बाद ये हाल हो गया कि जब इस्लामी फ़ौज किसी जगह उतरती तो उसके घने डेरे को देखकर ऐसा लगता कि अगर एक चादर तान दी जाए तो सब के सब उसके नीचे होंगे।
शोर और हंगामे का निषेध
अरब युद्ध में इतना शोर और हंगामा हुआ करता था कि उसका नाम ही ‘विग़ा’ (शोर) रख दिया गया था। इस्लाम लाने के बाद भी अरब इसी तरीक़े का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं:
“हम अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ थे, और जब हम किसी घाटी में पहुँचते थे, तो हम ज़ोर-ज़ोर से अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह के शुक्र के नारे लगाते थे। इस पर पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा, “लोगों! गरिमा के साथ चलो, जिसे तुम पुकार रहे हो, वह न तो बहरा है और न अनुपस्थित है, वह तुम्हारे साथ है, सब कुछ सुनता है और बहुत क़रीब है।”
बर्बर कृत्यों के ख़िलाफ़ सामान्य निर्देश
सेना के प्रस्थान के समय योद्धाओं के व्यवहार पर निर्देश देने की विधि, जिसे पश्चिमी दुनिया उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अनभिज्ञ थी, का आविष्कार अरब में इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) द्वारा सातवीं शताब्दी ई. में किया गया था। इस्लाम के पैग़म्बर (सल्ल.) का यह नियम था कि जब वे किसी सैन्य दल को युद्ध के लिए भेजते, तो पहले सेना को धर्मपरायणता और अल्लाह से डरने का उपदेश दिया करते, फिर कहते:
अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के मार्ग में, उन लोगों को क़त्ल करो जो अल्लाह का इनकार करते हैं।
“जाओ, अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह के रास्ते में उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ो जो अल्लाह की आज्ञापालन का इनकार करते हैं, लेकिन युद्ध में किसी से वचन-भंग न करना, विजयधन की चोरी न करना, ‘मुसला’ (अंग-विच्छेदन) न करना और किसी बच्चे की हत्या न करना।”
उसके बाद वे सेना को निर्देश देते कि दुश्मन के सामने तीन चीज़ें पेश करना, पहला इस्लाम, दूसरा जिज़्या और तीसरा युद्ध। अगर वह इस्लाम स्वीकार कर ले तो उस पर हाथ न उठाओ, अगर वह जिज़्या देकर अधीनता स्वीकार कर ले तो उसके जान-माल को कोई नुक़सान न पहुंचाओ, लेकिन अगर वह उससे भी इनकार कर दे, तो अल्लाह से मदद मांगो और युद्ध करो।
पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र ने जब सीरिया की ओर अपनी सेना भेजी तो उसे दस निर्देश दिए, जिनकी नक़ल सभी इतिहासकारों और हदीस के विद्वानों ने की है। वे निर्देश हैं:
(1) महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों की हत्या न की जाए।
(2) ‘मुसला’ (अंग-विच्छेदन) न किया जाए।
(3) भिक्षुओं और उपासकों को न सताया जाए और न उनके उपासनागृह ध्वस्त किए जाएं।
(4) किसी भी फलदार वृक्ष को नहीं काटा जाए और न खेतियां जलाई जाएं।
(5) बस्तियां न उजाड़ी जाएं।
(6) जानवरों को न मारा जाए।
(7) किसी भी स्थिति में वचनभंग न किया जाए।
(8) आज्ञा पालन करने वालों के जीवन और संपत्ति का उसी तरह सम्मान किया जाए जैसे मुसलमानों के जीवन और संपत्ति का।
(9) विजयधन में चोरी न की जाए।
(10) युद्ध में पीठ न फेरी जाए।
सुधार के परिणाम
इन फ़ैसलों के अध्ययन से पता चलता है कि इस्लाम ने उन सभी बर्बर प्रथाओं से युद्ध को मुक्त कर दिया जो उस युग में युद्ध के अभिन्न अंग बने हुए थे। राजदूतों और युद्धबंदियों की हत्या, समझौतों की अवहेलना, युद्ध में घायलों की हत्या, ग़ैर-लड़ाकों की हत्या, शवों का अपमान और अंगभंग, आग की यातना, लूटपाट और रास्तों का रोकना, फ़सलों और बस्तियों की बर्बादी। सेनाओं का फैलाव और अव्यवस्था, लड़ाई का कोलाहल, सभी को युद्ध के नियमों के ख़िलाफ़ ठहरा दिया गया, और युद्ध को केवल एक ऐसी चीज़ रह गई, जिसमें भला और बहादुर आदमी शत्रु के जहां तक संभव हो, कम से कम हानि पहुँचा कर उसकी बुराई को दूर करने का प्रयास करें।
सुधार की इस शिक्षा के 8 साल की छोटी अवधि में जो शानदार परिणाम आए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण मक्का की विजय है। एक शक्ति पर दूसरी शक्ति की जीत और विशेष रूप से दुश्मन के एक बड़े शहर की विजय के अवसर पर बर्बर अरब में ही नहीं, बल्कि सभ्य रोम और ईरान में भी जो कुछ होता था, उसे ध्यान में रखिए और विचार कीजिए कि वही अरब जो कुछ ही साल पहले तक असभ्य और बर्बर तौर-तरीक़ों के आदी थे, उस नगर में विजेता के रूप में प्रवेश करते हैं जहां से उन्हें आठ साल पहले बुरी तरह प्रताड़ित कर के खदेड़ दिया गया था, और उन्हीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने उनको उनके घरों से बेघर करने पर ही बस नहीं किया था, बल्कि जहां उन्होंने जाकर शरण ली थी, वहां से भी उन्हें खदेड़ने के लिए कई बार चढ़ाई कर चुके थे। ऐसे शहर और ऐसे दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है, लेकिन कोई नरसंहार नहीं होता है, कोई लूटपाट नहीं होती है, किसी के जीवन,संपत्ति, मान और सम्मान पर हमला नहीं होता है, पुराने और और जानी दुश्मनों में से किसी पर बदले का हाथ नहीं उठता। पूरी कार्वाई में केवल 24 लोग मारे जाते हैं और वे भी ऐसे लोग जिन्होंने ख़ुद आगे बढ़ कर तलवार चलाई थी। शहर में प्रवेश करने से पहले सेनानायक यह घोषणा कर देता है कि जब तक कोई तुम पर हाथ न उठाए तब तक तुम भी हाथ न उठाना। शहर में प्रवेश करते ही यह उपदेश दिया जाता है कि जो अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए वह सुरक्षित है, जो कोई आत्मसमर्पण कर दे, वह सुरक्षित है और जो अबू सुफ़ियान के घर में शरण लेता है वह भी सुरक्षित है। फिर, विजय के पूरा होने के बाद, उन दुश्मनों को एक-एक करके विजयी सरदार के सामने लाया जाता है, जिन्होंने उसे इसी शहर में तेरह साल तक यातनाएँ दीं और अंत में उसे निर्वासन के लिए मजबुर कर दिया, जो उसे और उसके धर्म को दुनिया से मिटाने के लिए बद्र, उह्द और अहज़ाब में बड़ी तैयारियाँ करके गए थे, ये दुश्मन सिर झुकाए आकर खड़े होते हैं। विजेता पूछता है, “अब तुम क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? विजित सिर झुकाकर जवाब देते हैं,” तुम उदार हृद्य वाले भाई और उदार हृद्य वाले भाई के बेटे हो। इसपर विजेता कहता है, जाओ तुम आज़ाद हो आज तुम से कोई पूछताछ नहीं। केवल उनकी जान ही नहीं बख़्शी गई, बल्कि विजेता और उसकी सेना ने उन संपत्तियों को भी उनके पक्ष में माफ़ कर दिया जिससे 8 साल पहले वे बेदख़ल किए गए थे।
हालांकि इनमें कुछ ऐसे भी घोर शत्रु थे जिनके द्वारा पहुंचाया गया कष्ट हद से बढ़कर था। विजेता की जवान बेटी सैय्यदा ज़ैनब के हत्यारे हिबार बिन असवद ने विनम्रतापूर्वक इस्लाम क़ुबूल कर लिया और उसे माफ़ कर दिया गया। विजेता के प्यारे चाचा को मारने वाला वहशी बिन हर्ब मुसलमान बन गया और उसे माफ़ कर दिया गया। हिंद बिन्त उत्बाह, जो हज़रत हमज़ा की किडनी चबा गई थी, अपनी अत्यधिक क्रूरता के बावजूद, विजेता के क्रोध से सुरक्षित थी। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, अबू जह्ल का बेटा इकरिमा, जो ख़ुद भी इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, मुसलमान बन गया और अल्लाह के रसूल के साथियों में शामिल हो गया। उनके अलावा, और भी कई जो विजेता के जानी दुश्मन थे, को क्षमा कर दिया गया।
ये वो सुधार था जो दुनिया के सबसे बर्बर समुदाय में केवल 8 साल में किया गया। आज सभ्यता के इस युग में भी जब विश्व के सबसे सभ्य राष्ट्र शत्रु के नगर में विजयी होकर प्रवेश करते हैं, तो जीते हुए नगर पर किस प्रकार अत्याचार होते हैं, यह सभी जानते हैं। 20वीं सदी के पहले और दूसरे विश्व युद्ध में पश्चिमी सभ्यता के अग्रदूतों ने एक दूसरे के देश पर आक्रमण करके जो तबाही मचाई है, उसके दृश्य देखने वाली आंखों में आज भी मौजूद हैं। इसके विपरीत ग़ौर कीजिए कि 14 सौ साल पहले के अन्धकार युग में जबकि दुनिया की सभ्यता का झंडा ख़ुसरो परवेज़ और हर्कुलिस जैसे राजाओं के हाथ में था, अरब के एक अशिक्षित और असभ्य राष्ट्र ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों के शहर में प्रवेश करके जो सभ्य और शालीन व्यवहार किया, वह कितने बड़े सुधार, कितने उच्च नैतिक प्रशिक्षण और कितने सही और मज़बूत सैन्य अनुशासन का परिणाम हो सकता था।
(4) युद्ध के सभ्य क़ानून
यह उन चीज़ों का उल्लेख था जो दुनिया में प्रचलित थीं और इस्लाम ने उन पर प्रतिबंध लगाया। अब हम उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो दुनिया में नहीं थीं और इस्लाम ने उन से परिचित कराया। हमें यह देखना है कि युद्ध के ग़लत तरीक़ों को रोककर इस्लाम ने किस तरह के क़ानून स्थापित किये, इसके लिए हम केवल उन सैद्धांतिक क़ानूनों को ही लेंगे जिन पर युद्ध के क़ानून आधारित हैं, बाक़ी रहे अमौलिक आदेश तो वे उस समय के विद्वानों पर छोड़ दिए गए हैं कि वे अपने समय की ज़रूरतों के अनुसार मूल सिद्धांतों और नियमों से निकालें।
कमांडरों के प्रति निष्ठा
युद्ध को एक संहिता के तहत लाने में इस्लाम का पहला कार्य यह था कि इस ने सैन्य प्रणाली को केंद्रीकृत किया और सेना में आज्ञाकारिता का एक मज़बूत क़ानून जारी किया। इस्लाम के युद्ध के नियमों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि कमांडर की अनुमति के बिना कोई छोटी से छोटी सैन्य कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। दुश्मन को मारना, उसकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा करना, उसे क़ैद करना, उसके युद्ध उपकरणों को नष्ट करना अपने आप में जायज़ है, लेकिन यह ऐसी स्थिति में अपराध हो जाता है जब कमांडर के आदेश और अनुमति के बिना ऐसा किया जाए। बद्र की लड़ाई से पहले, जब अब्दुल्ला बिन जहश ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की अनुमति के बिना क़ुरैश के एक समूह के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और कुछ माल लूट लाए, तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने नाराज़गी व्यक्त की और लूट के माल को अवैध ठहराया। सहाबा के समूह ने उन्हें यह कहकर फटकार लगाई, “तुमने वह काम किया है जिसका तुम्हें आदेश नहीं दिया गया था।” हज़रत ख़ालिद बनी जज़ीमा की ओर इस्लाम का पैगाम लेकर भेजे गये था और वहां उन्होंने इमाम की अनुमति के बिना, एक ग़लतफ़हमी के आधार पर हत्या कर दी। जब अल्लाह के रसूल को इसकी सूचना मिली, तो वे ग़ुस्से में खड़े हो गए और हज़रत अली को आज्ञा दी कि जाओ और अज्ञानता के काम को मिटा दो। (फ़त्हुल-बारी: खंड 8, पृष्ठ 42)
इस्लाम ने इमाम की आज्ञाकारिता को स्वयं अल्लाह और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की आज्ञाकारिता के बराबर ठहराया है, और इमाम की अवज्ञा को अल्लाह के दूत की अवज्ञा के समान दर्जा दिया है। हदीस में इसका उल्लेख है:
युद्ध दो प्रकार के होते हैं। एक वह जब व्यक्ति विशेष अल्लाह की ख़ुशी प्राप्त करने के लिए लड़ता है, इमाम की आज्ञा का पालन करता है, अपना सबसे अच्छा माल ख़र्च करता है और फ़साद से बचता है। उसका सोना और जागना इनाम का हक़दार है। और जिस किसी ने दिखावे और प्रसिद्धि के लिए लड़ाई की, इमाम की अवज्ञा की और ज़मीन में फ़साद फैलाया, तो वह बराबर भी नहीं छूटेगा।”
एक दूसरी हदीस में है :
“जो मेरी बात मानता है वह अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है और जो मेरी अवज्ञा करता है वह अल्लाह की अवज्ञा करता है, फिर जो अमीर की बात मानता है वह मेरी बात मानता है और जो अमीर की अवज्ञा करता है वह मेरी अवज्ञा करता है।”
इन आदेशों ने युद्ध में एक नियमितता पैदा कर दी। यह केवल एक ख़ूनी खेल नहीं रहा कि सेना का हर सदस्य लोगों के जीवन और संपत्ति का स्वामी और लूट एवं हत्या के लिए अधिकृत हो। इस्लामपूर्व ज़माने में फ़ौज के सिपाही सरेआम लूटपाट करते थे और दुश्मन राज्य में घुसने के बाद हर फ़ौजी को हक़ था कि वह जिसे चाहे क़त्ल कर दे, जिसे चाहे लूट ले, किसी गाँव और खेत को आग लगा दे और शत्रु राष्ट्र को नष्ट करने के लिए जो चाहे करे। स्वयं सिकंदर की सेना, जिसका अनुशासन सर्वविदित है, इस प्रथा से अलग नहीं थी। उसके सैनिकों ने ईरान में आगे बढ़ते हुए जिस आज़ादी के साथ देश को तहस-नहस कर दिया, वह इतिहास में संरक्षित है। लेकिन इस्लाम द्वारा सेना के लिए जो नियम और सिद्धांत निर्धारित किए गए उनमें, सैनिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रता देने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम के अनुसार मानव रक्त बहाने की ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता है और हर व्यक्ति इसके औचित्य और अनौचित्य को तय नहीं कर सकता। इस्लामी क़ानून में, एक “अमीर” को युद्ध के सभी कार्यों के लिए ज़िम्मेदार बनाया गया और आदेश और निषेध के सारे अधिकार उसी के पास हैं। और उसकी पूरी आज्ञाकारिता सेना पर अनिवार्य कर दी गई है। एक सैनिक को इतना अधिकार भी नहीं दिया गया है कि वह अमीर की अनुमति के बिना शत्रु की भूमि से किसी वृक्ष का एक फल भी तोड़कर खाले।
शपथ और समझौतों का सम्मान
इस्लामी क़ानून ने युद्ध और शांति दोनों में वादा निभाने पर बहुत ज़ोर दिया है। इस्लाम की सच्ची नैतिकता के मुख्य नियमों में से एक यह है कि व्यक्ति को सख़्त से सख़्त ज़रूरत में भी अपने वादे पर क़ायम रहना चाहिए। वादा तोड़ने से कितना ही बड़ा फ़ायदा क्यों न हो और वादा पूरा करने से कितना ही बड़ा नुक़सान क्यों न हो, इस्लाम अपने मानने वालों को इस फायदे को छोड़ देने और इस नुक़सान को सहन करने की ताकीद करता है, क्योंकि वादा तोड़ने से कभी उतना बड़ा लाभ नहीं हो सकता जिससे किसी व्यक्ति की नैतिकता और आध्यात्मिकता को होने वाले नुक़सान की भरपाई हो सके। प्रतिबद्धता का बड़ा से बड़ा नुक़सान इसके साथ आने वाले नैतिक और आध्यात्मिक लाभ को कम नहीं कर सकता है। जिस तरह यह नियम व्यक्तिगत और निजी जीवन पर लागु होता है, उसी तरह यह सामूहिक और राष्ट्रीय जीवन पर भी आच्छादित है। आजकल संसार में यह नियम हो गया है कि बहुत से कार्य ऐसे हैं, जिनको व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्थिति में अत्यंत शर्मनाक मानता है, लेकिन राष्ट्र उसे अपनी सामूहिक स्थिति में सही मानते हैं और उसमें दोष नहीं मानते। लगभग सभी राज्य अपने साम्राज्य के विकास और अपने राष्ट्र के हित के लिए, झूठ, बेईमानी, वचन भंग आदि की अनुमति देते हैं। लेकिन इस्लाम इस मामले में व्यक्ति और समुदाय, आम नागरिक और सत्ताधारी वर्ग, व्यक्ति और राष्ट्र के बीच कोई अंतर नहीं करता है, और हर हाल में अनुचित संचालन को नाजायज़ ठहराता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए हो या राष्ट्रीय हित के लिए।
وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًۭا تَتَّخِذُونَ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ (النحل: ۹۱-۹۲)
“अल्लाह का वादा पूरा करो जब तुम किसी के साथ अनुबंध करते हो। और अपनी क़समों को मज़बूत करने और अल्लाह को उस पर गवाह बनाने के बाद न तोड़ो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी ख़बर है। उस औरत की तरह मत बन जाओ, जिसने अपना ही काता हुआ सूत मेहनत से कातने के बाद उसे टुकड़े-टुकड़े कर डाला। तुम अपनी शपथों को आपसी विश्वासघात के रूप में इस्तेमाल करते हो ताकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से धन और सम्मान में बढ़ जाए।” (अल-नहल: 91-92)
इसी विषय की कई आयतें पवित्र क़ुरआन में आई हैं। यहाँ उन सभी को कवर करने का इरादा नहीं है, केवल कुछ को उद्धृत किया जाता है:
ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَـٰقَ ○ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ ۔۔۔أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ○ (الرعد :۲۰-۲۲)
“जो अल्लाह के वचन को निभाते हैं और समझौता को नहीं तोड़ते और अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे स्थापित करते हैं। उन के लिए अच्छा अंजाम है।” (अल-रअद: 21-22)
بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ○ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًۭا قَلِيلًا أُو۟لَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ○ (آل عمران: ۷۶-۷۷)
“क्यों नहीं, जिसने अपना वचन पूरा किया और (अल्लाह से) डरा, तो वास्तव में अल्लाह डरने वालों को पसंद करता है। निःसंदेह जो अल्लाह के वचन तथा अपनी क़समों को थोड़े मूल्य पर बेच डालते हैं, उन के लिए आख़िरत (परलोक) में कोई इज़्ज़त नहीं, अल्लाह क़ियामत के दिन न उनसे बात करेगा और न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पवित्र करेगा तथा उन्हीं के लिए दुःखदायी यातना है।” (आले इमरान:76-77)
ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ○ (البقرہ :۱۷۷)
“और जो लोग वादा करके अपना वादा निभाते हैं, और जो बुरे समय और युद्ध की स्थिति में जमे रहते हैं, वही सच्चे लोग हैं और वही नेक हैं।” (अल-बकरा: 177)
وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ (الانعام: ۱۵۲)
“जब तुम बोलो, तो इंसाफ़ की बात बोलो, भले ही वह आदमी जिसके ख़िलाफ़ तुम कह रहे हो, यद्यपि वह तुम्हारा समीपवर्ती ही क्यों न हो और अल्लाह का वचन पूरा करो, उसने तुम्हें इसका आदेश दिया है, संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो।” (अनआम: 152)
وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًۭا ○ (بنی اسرائیل : ۳۴)
“वादा पूरा करो, क्योंकि वादों के बारे में पूछा जाएगा।”
इस शिक्षा का जो व्यावहारिक उदाहरण अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपनी जीवनी में प्रस्तुत किया, उसके अध्ययन से पता चलता है कि इस्लाम में समझौता का क्या मूल्य है। बद्र की लड़ाई में, जब अवज्ञाकारियों की संख्या मुसलमानों की संख्या से तीन गुना थी और मुसलमानों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक-एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, हुजैफ़ा बिन अलीमान और उनके पिता हसील बिन जाबिर इस्लाम की सेना की ओर रवाना हुए। रास्ते में अवज्ञाकारियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम ज़रूर मुहम्मद की मदद करने जा रहे होगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मदीना जाने का इरादा है। इस पर अवज्ञाकारियों ने उन्हें युद्ध में भाग न लेने की प्रतिज्ञा देकर छोड़ दिया। ये दोनों सज्जन अवज्ञाकारियों के चंगुल से छूटकर बद्र के मैदान में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के पास पहुंचे और उनके साथ जो हुआ था उसे दोहराया। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने यह सुनकर आदेश दिया, “तुम मदीना चले जाओ, हम अहद पूरा करेंगे और हम अल्लाह से उनके ख़िलाफ़ मदद मांगेंगे।”
हुदैबिया की संधि में क़ुरैश के साथ जो शर्तें तय हुई थीं, उनमें से एक यह थी कि अगर कोई व्यक्ति मक्का से भागकर मुसलमानों के पास जाता है, तो मुसलमान उसे वापस कर देंगे, और अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मक्का जाता है, तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। यह समझौता अभी लिखा ही जा रहा था कि अबू जिंदल बिन सुहैल किसी तरह मक्का के अवज्ञाकारियों की क़ैद से भाग निकले और इस्लाम की फ़ौज में पहुंच गये। पांवों में बेरियां थीं, बदन पर मार के निशान थे, चेहरे पर सख़्त तकलीफ़ के निशान थे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के सामने फ़रियाद करने लगे कि अल्लाह के वास्ते मुझे इस मुसीबत से निकालिए। मुसलमान उनकी हालत देखकर व्याकुल हो उठे। चौदह सौ तलवारें अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के एक इशारे की प्रतीक्षा में थीं और इस्लामी भाईचारा एक मुस्लिम भाई को क़ैद से छुड़ाने के लिए बेचैन था। लेकिन शांति की शर्तें तय हो चुकी थीं, अनुबंध लिखा जा रहा था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने अबू ज़िंदाल को रिहा करने से साफ़ इनकार कर दिया और कहा: “अबू ज़िंदाल! सब्र रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए छुटकारे का रास्ता ज़रूर निकालेगा।”
जब वे मदीना लौटे, तो एक अन्य साथी, अबू बसीर, मक्का के अवज्ञाकारियों की क़ैद से भाग निकले और नबी के पास पहुंचे। उनके पीछे अवज्ञाकारी भी दो आदमियों के साथ पहुंचे और अबू बसीर की वापसी की मांग करने लगे। पैग़म्बर (सल्ल.) जानते थे कि मक्का में मुसलमानों के साथ कैसा क्रूर व्यवहार होता है और विशेष रूप से भागे हुए क़ैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, लेकिन समझौता सबसे ऊपर था उन्होंने मुसलमानों को अत्याचारियों के हवाले कर दिया लेकिन समझौते को तोड़ना पसंद नहीं किया।
नबुव्वत और सहाबा के ज़माने में इस तरह की अनगिनत घटनाएं मिलती हैं, जिन्हें यहां समेटना मुश्किल है।
तटस्थ पक्ष के अधिकार
इस्लाम में तटस्थता की शब्दावली नहीं है, बल्कि इसे अनुबंध के तहत शामिल किया गया है। इस्लामी क़ानून सभी ग़ैर-मुस्लिम समुदायों को दो दलों में विभाजित करता है। एक जिसके साथ अनुबंध है, दूसरा जिसके साथ कोई अनुबंध नहीं है। अनुबंध वाले राष्ट्र जब तक अनुबंध की शर्तों पर रहेंगे, तब तक उनके साथ शर्तों के अनुसार ही मामला किया जाएगा और युद्ध में उन पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया जाएगा। यही तटस्थता का अर्थ है। बाक़ी रहे ऐसे राष्ट्र जिनके साथ कोई अनुबंध न हो, उनके साथ युद्ध हो या न हो, वे युद्धरत ही माने जाएंगे क्योंकि इस्लाम ने अनुबंध वाले राष्ट्र और ऐसे राष्ट्र जिनके साथ कोई अनुबंध न हो, के बीच किसी भी मध्य मार्ग को मान्यता नहीं दी है।
अनुबंध वाले राष्ट्रों के साथ सभी मामले अनुबंध की शर्तों के अधीन होंगे, लेकिन इस्लाम ने युद्ध के मामलों में अनुबंध वाले राष्ट्रों के लिए कुछ सैद्धांतिक अधिकार भी निर्धारित कर दिए हैं जो इस प्रकार हैं:
(1) जब तक अनुबंध वाले राष्ट्र अनुबंध पर स्थापित हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना मुसलमानों के लिए सख़्त वर्जित है:
إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَمْ يُظَـٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًۭا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ○ (التوبه : ۴)
“परन्तु जिन बहुदेववादियों से तुम ने समझौता किया था, और जिन्होंने उसके पालन में कोई कमी नहीं की, और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, उन से समझौता की अवधि के समाप्त होने तक समझौता का पालन करो, क्योंकि अल्लाह परहेज़गार लोगों को पसंद करता है।” (अत्तौबा :4)
(2) अगर मुसलमानों का एक समूह किसी अनुबंध वाले देश में बसा हुआ हो और उन पर अत्याचार हो रहा हो, तो इस्लामी राज्य उन मुसलमानों का समर्थन नहीं कर सकता है:
وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ○ (الانفال: ۷۲)
“ग़ैरमुस्लिम देश में रहने वाले मुसलमान यदि वे धर्म के बारें में तुमसे सहायता मांगें, तो तुमपर उनकी सहायता करना आवश्यक है। परन्तु किसी ऐसे राष्ट्र के विरुध्द नहीं, जिनके और तुम्हारे बीच संधि हो तथा तुम जो कुछ कर रहे हो, उसे अल्लाह देख रहा है।” (अल-अनफ़ाल:72)
(3) युद्ध की स्थिति में, अनुबंधित राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। अगर शत्रु भागकर ऐसे देश की सीमा में शरण ले ले तो इस्लामी सेना वहाँ उसका पीछा नहीं कर सकती :
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ (النساء ۸۹-۹۰)
“और अगर यह दल बाज़ न आए, तो उन्हें पकड़ो और जहां कहीं पाओ मारो, और उन्हें अपना मित्र और सहायक न बनाओ, सिवाय उन लोगों के जो उस राष्ट्र से जा मिलें, जिनके साथ तुम्हारा समझौता हो।” (अन्निसा:89-90)
ये नियम और सिद्धांत तटस्थता के क़ानून का आधार हैं। ज़रूरत के नुसार इनसे आंशिक आदेश निकाले जा सकते हैं।
युद्ध की घोषणा
जब कोई राष्ट्र संधि की शर्तों का उल्लंघन करता है और इस्लामी राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाता है, तो इस्लामी क़ानून यह है कि उसे एक औपचारिक अल्टीमेटम दिया जाएगा, और अनुबंध को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद युद्ध छेड़ा जाएगा।
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةًۭ فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ○(الانفال :۵۸)
“और अगर तुम्हें किसी राष्ट्र से बेईमानी और विश्वासघात का डर हो, तो उनका अनुबंध समानता को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर फेंक दो।” (अनफ़ाल: 58)
समानता को ध्यान में रखते हुए अनुबंध को फेंकने का अर्थ यह है कि उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि तुम्हारे शत्रुतापूर्ण कार्य ऐसे हैं कि तुम्हारे साथ हमारा अनुबंध अब मान्य नहीं है। उसके बाद देखना चाहिये कि वे अपने रवैये से बाज़ आते हैं या नहीं, अगर फिर भी न बाज़ आये तो उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाय। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं: अगर वे फिर से नहीं रुके, तो उनके ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया जाना चाहिए।
इस्लाम के विद्वानों ने केवल सूचित करना ही पर्याप्त नहीं समझा है, बल्कि अनुबंध का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को राहत देने की भी सिफ़ारिश की है, ताकि अगर वह अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को ठीक करना चाहे, तो ऐसा कर सके।
इस बारे में हज़रत उमर का यह भी फ़ैसला है कि क़रार तोड़ने वालों को काफ़ी मोहलत दी जाए। उनकी ख़िलाफ़त के ज़माने में उमैर बिन सअद ने लिखा है कि हमारे इलाक़े में ग़र्बसौस एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हमारी ख़ुफ़िया ख़बरें दुश्मन तक पहुंचाते हैं और हमें दुश्मन की ख़बरें नहीं देते। इस पर हज़रत उमर ने उन्हें लिखा कि पहले तुम जाकर उनसे कहो कि हम तुम्हें एक बकरी की जगह दो बकरियां और एक गाय की जगह दो गायें देंगे और इसी तरह हर चीज़ के बदले दुगनी चीज़ें देंगे, तुम इस स्थान को छोड़ दो। अगर वे मान जाएं तो बेहतर है, नहीं तो उन्हें सूचित कर दो कि तुम्हारे साथ हमारा समझौता ख़त्म हो गया। फिर उन्हें एक साल की मोहलत दो और जब वह अवधि पूरी हो जाए तो उन्हें वहां से निकाल दो। (फ़त्हुल-बलदान: पृष्ठ 162-163)
युद्धबन्दी
ऊपर कहा जा चुका है कि इस्लाम युद्ध बंदियों की हत्या को निषिद्ध ठहराता है। इस्लामी क़ानून में उनके लिए केवल इतनी ही सुविधा नहीं है कि उनकी हत्या न की जाए, बल्कि उनके प्रति बेहद नरमी बरतने का भी आदेश है। क़ुरआन में क़ैदियों, यतीमों और अभावग्रस्तों को खाना खिलाने की प्रेरणा दी गई है और उसे भले लोगों का काम बताया गया है:
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ○ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ○ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا○ (الدھر:۸-۱۰)
“वे ग़रीबों, अनाथों और बंदियों को अल्लाह की ख़ुशी के लिए खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तो केवल अल्लाह के लिए तुम्हें खिलाते हैं, हम कोई इनाम या आभार नहीं चाहते हैं, हम तो केवल उस कठिनाई के दिन से डरते हैं, जिसमें अत्यधिक पीड़ा के कारण चेहरे विकृत हो जाएंगे।” (अल-दह्र :8-10)
पैग़म्बर (सल्ल.) हमेशा क़ैदियों के प्रति अच्छे व्यवहार का उपदेश देते थे। बद्र की लड़ाई में जब वे लोग पकड़ कर लाए गए, जिन्होंने मुसलमानों को 13 सालों तक प्रताड़ित करके शहर छोड़ने पर विवश किया था, तो नबी ने अपने साथियों से उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की। साथियों ने इस आदेश का पालन करते हुए उन्हें अपने से बेहतर खाना खिलाया और अपने से ज़्यादा आराम दिया। कुछ सहाबी ख़ुद खजूर खाते थे और क़ैदियों को रोटी और सालन खिलाते थे। क़ैदियों के पास जब कपड़े न होते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास से कपड़े पहनाए, हालाँकि वह ज़माना मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल का ज़माना था। उन क़ैदियों में से एक, सुहैल बिन अम्र, एक बहुत ही वाक्पटु वक्ता था और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के ख़िलाफ़ जहरीला भाषण देता था। हज़रत उमर ने सुझाव दिया कि उसके दांत तोड़ दिए जाएं, लेकिन पैग़म्बर (सल्ल.) ने कहा कि “अगर मैं उसके साथ ऐसा करता हूं, तो अल्लाह मेरे साथ भी यही करेगा।” कुछ समय तक क़ैद में रखने के बाद, उन सभी क़ैदियों को फिरौती लेकर रिहा कर दिया गया।
युद्धबंदियों के बारे में इस्लामी क़ानून यह है कि युद्ध के अंत में, उन्हें या तो फिरौती लेकर या फिरौती के बिना रिहा कर दिया जाए, या क़ैद में रख कर उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए:
فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا۟ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً○ (محمد:۴)
“जब अवज्ञाकारियों से तुम्हारी मुठभेड़ हो, तो पहले उन्हें तब तक मारो जब तक तुम उन्हें हरा न दो, फिर क़ैद के बंधन को मज़बूत करो, उसके बाद तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम उनपर उपकीर करो या उन्हें फिरौती लेकर रिहा कर दो।” (मुहम्मदः 4)
इस आयत के अनुसार अल्लाह के रसूल अक्सर युद्धबंदियों को बिना फिरौती लिए रिहा कर देते थे। मक्का के 80 लोगों ने जबल तनीम में इस्लामी सेना पर हमला किया और उन सभी को पकड़ लिया गया। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उन सभी को बिना फिरौती के छोड़ दिया। हुनैन के युद्ध में ह्वाज़न के 6,000 क़ैदियों को इसी तरह रिहा किया गया था। यमामा के प्रमुख समामा बिन असाल को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे भी बिना फिरौती के रिहा कर दिया गया। इससे वह इतना प्रभावित हुआ कि वह मुसलमान हो गया। हालाँकि, कभी-कभी फिरौती भी ली जाती थी, ख़ासकर कठिनाई के समय में।
ग़ुलामी की समस्या
इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि इस्लाम द्वारा युद्धबंदियों को दास और दासियां बनाने की जो अनुमति दी है तथा युद्ध में बन्दी महिलाओं से सम्बन्ध स्थापित करने को जायज़ रखा है, उसकी क्या वास्विकता है? और अगर यह मुद्दा वास्तव में इस्लाम में मौजूद है, तो यह युद्ध बंदियों के बारे में क़ुरआन के क़ानून की भावना के कहां तक अनुरूप है? इसके कारण और उत्पत्ति को समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
सर्वप्रथम इस युग में युद्धबंदियों के आदान-प्रदान की कोई नीति नहीं थी। जब मुस्लिम पुरुषों को अन्य राष्ट्रों द्वारा क़ैद किया जाता था, तो उन्हें ग़ुलामों के रूप में रख लिया जाता था, इसलिए मुसलमानों के पास भी इस के सिवा कोई विकल्प नहीं था, कि दुश्मन देशों के बंदियों को ग़ुलामों के रूप में रखा जाए। हालाँकि, जहाँ भी विनिमय का अवसर पैदा हुआ है, मुसलमानों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अल्लामा इब्न हजर फ़त्हुल-बारी (खंड 2, पृष्ठ 101) में लिखते हैं कि “अगर मुसलमानों के पास बहुदेववादियों के क़ैदी होते और बहुदेववादियों के पास मुसलमानों के क़ैदी होते और उनके संबंधित क़ैदियों को रिहा करने पर सहमति हो जाती, तो ऐसा कर लिया जाता।
दूसरे यह कि कभी-कभी किसी शहर के अधिकांश पुरुष युद्ध में काम आ जाते थे, और कभी-कभी एक शहर के सभी पुरुष जो हथियार उठा सकते थे, मारे जाते थे। ऐसी स्थिति में परित्यक्त महिलाओं और बच्चों की देखभाल का प्रबंध इसके सिवा किसी अन्य तरीक़े से नहीं हो सकता था कि इसकी ज़िम्मेदारी स्वयं विजेता राष्ट्र अपने ऊपर लेले। जब विजेताओं ही को यह काम करना था तो महिलाओं की सुरक्षा और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए इस से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता था कि मुस्लिम पुरुषों को उनसे दाम्पत्य संबंघ बनाने की अनुमति दे दी जाए। इस तरह, वे इस्लामी समाज की सदस्य बन गईं और उन बुराइयों के दरवाज़े बंद हो गये जो हज़ारों महिलाओं के पतिहीन होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से खुल जाते हैं।
तीसरे, इस्लाम ने युद्धबंदियों को ग़ुलाम बनाने की केवल अनुमति दी है, आदेश नहीं दिया है। इस अनुमति का लाभ उठाना या न उठाना मुसलमानों का ऐच्छिक कार्य है, बल्कि सच्चे ख़लीफ़ाओं के व्यवहार से यह स्पष्ट होता है कि लाभ न उठाना ही बेहतर है। मिस्र, सीरिया, इराक़, अफ्रीका, आर्मेनिया और फ़ारस की विजय में, असंख्य स्थानों पर विजय प्राप्त की गई और उनके लाखों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन एक छोटी संख्या के सिवा किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया गया। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि एक सेनानायक ने लोगों को ग़ुलाम बना लिया और जब ख़लीफ़ा को इस बारे में पता चला तो उसने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि मिस्र के कुछ गाँवों को भयंकर प्रतिस्पर्धा के बाद जीत लिया गया और मुसलमानों ने उनके निवासियों को ग़ुलाम बना लिया और उन्हें हज़रत उमर के पास मदीना भेज दिया, लेकिन हज़रत उमर ने उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें उनके वतन लौटा दिया। इससे पता चलता है कि युद्धबंदियों को ग़ुलाम बनाना आवश्यक या वांछनीय नहीं था, बल्कि उसे एक अपरिहार्य बुराई के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि दास विनिमय का कोई नियम मौजूद नहीं था।
चौथा, इस्लाम मजबूरी की हालत में केवल उन लोगों को ग़ुलाम बनाने की अनुमति देता है जो युद्ध में पकड़े हुए आएं। बाक़ी मुक्त लोगों को पकड़ कर बेचना, जो उस ज़माने में प्रचलित था, इस्लाम ने उसे सख़्ती के साथ रोक दिया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा:
“तीन आदमी ऐसे हैं जिन पर क़ियामत के दिन मैं ख़ुद मुक़द्दमा करूँगा, एक जिसने मेरा ज़िम्मा देकर वचनभंग किया, दूसरा वह जिसने आज़ाद इन्सान को बेच कर उसकी क़ीमत खाई, तीसरा वह जिसने किसी मज़दूर से पूरा काम लिया और उसकी मज़दूरी न दी।” (बुख़ारी)
उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को कुछ महत्वपूर्ण मजबूरियों के चलते जायज़ रखा था। उस तरीक़े को अगर पूर्ण रूप से जारी रखा जाता तो संभव था कि मुसलमानों के बीच भी ग़ुलामों का एक वर्ग पैदा हो जाता, जैसा कि इस्लामपूर्व अरब में, और रोम और ईरान जैसे देशों में प्रचलित था। शायद भारत के शूद्रों की तरह सबाया मुसलमानों में भी एक अलग जाति बन जाती। लेकिन इस्लाम का नियम यह है कि जिन मामलों में सीधे तौर पर सुधार करना मुश्किल होता है, वह उन्हें रखता तो है, लेकिन उन्हें ज्यों का त्यों रहने नहीं देता, बल्कि परोक्ष सुधार के ऐसे तरीक़े अपनाता है, जिससे उसके सारे नुक़सान दूर हो जाते हैं। ग़ुलामी के मुद्दे पर भी ऐसा ही किया गया। कुछ कारणों से ग़ुलामी को मिटाना मुश्किल था, इसलिए उसने बाहरी रूप में उसे रखते हुए अप्रत्यक्ष तरीक़ों से उसके मूल को इस तरह बदल दिया कि यह एक गंभीर सामाजिक बुराई के बजाय एक अद्भुत मानवीय लाभ बन गया। इस उद्देश्य के लिए इस्लाम ने कई तरीक़े अपनाए हैं, जिनमें से तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं।
(1) ग़ुलाम को मुक्त करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने को एक बड़ा सवाब (पूण्य कार्य) बताया और हर तरह से इसे प्रोत्साहित किया। क़ुरआन में इसका उल्लेख है:
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۔ فَكُّ رَقَبَةٍ ۔ أَوْ إِطْعَـٰمٌۭ فِى يَوْمٍۢ ذِى مَسْغَبَةٍۢ ۔ يَتِيمًۭا ذَا مَقْرَبَةٍ ۔ أَوْ مِسْكِينًۭا ذَا مَتْرَبَةٍۢ۔ (البلد :۱۲-۱۶)
“और तू क्या जानता है कि नेकी का कठिन मार्ग कौन सा है? वह यह कि एक गर्दन (यानी एक ग़ुलाम की गर्दन) को मुक्त की जाए या भूख के दिन में किसी पास के अनाथ या बेसहारा ग़रीब को खाना खिलाया जाए।” (अल-बलद: 12 - 16)
एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग्रामीण अरब आया और बोला, “या अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा काम बताइ जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो सकूँ। उन्होंने कहा: “ग़ुलाम को आज़ाद करो और ग़ुलामी से गर्दनें छुड़ाओ।” एक और हदीस में है कि नबी ने कहा, जिसने भी एक मुस्लिम ग़ुलाम को मुक्त करेगा तो उसका हर अंग उस ग़ुलाम के हर अंग के बदले नरक की आग से बच जाएगा।
दासों को मुक्त करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, नबी (सल्ल.) ने यह नियम स्थापित किया कि दास जितना अधिक मूल्यवान और अधिक इष्ट होगा, उतना ही बड़ा पूण्य होगा। हज़रत अबूज़र ने पूछा, कैसे ग़ुलाम को मुक्त कराना बेहतर है? उन्होंने कहा, “जिसकी क़ीमत अधिक हो और जिसे मालिक द्वारा अधिक पसंद किया जाता हो।” इसी तरह, उन्होंने दासी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके आज़ाद करने और उससे निकाह कर लेने को महान भलाई का कार्य ठहराया।
“फिर विभिन्न गुनाहों के जो प्रायश्चित निर्धारित किए गए हैं उनमें ग़ुलामों को मुक्त कराने को सबसे अच्छा प्रायश्चित बताया गया है। मुसीबतों को दूर करने के साधन के तौर पर भी ग़ुलामों को मुक्त कराने पर प्रोत्साहित किया गया है।
2. दूसरा तरीक़ा यह था कि दासों के साथ दया और सज्जनता पर अत्यधिक बल दिया गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी उम्मत को जो वसीयत की, उसमें पहले नमाज़ पर ज़ोर दिया गया और फिर दासों के साथ दया और सदव्यवहार पर। ग़ुलामी की अवधारणा अज्ञानकाल से मन में घर कर गई थी, जिसके प्रभाव से कभी-कभी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथी दासों के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते थे। इस पर उन्होंने अपने परम आदरणीय साथियों को कई बार फटकार भी लगाई है।
एक बार उन्होंने अबूज़र ग़िफ़ारी से कहा, “अभी तुम से अज्ञान निकला नहीं है। याद रखो कि ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे सेवक हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारा अधीन बनाया है। इसलिए जिस किसी का भाई उसके अधीन हो उसे चाहिए कि उसको वही खिलाए जो वह ख़ुद खाता है और वही पहनाए जो पहनता हो। उनकी शक्ति से अधिक उन पर बोझ न डाले और अगर उन्हें कोई भारी काम सौंपता हो, तो उनकी सहायता करे।”
एक बार एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हमें अपने सेवक को कितनी बार क्षमा कर देना चाहिए, अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उत्तर दिया, “अगर वह दिन में सत्तर बार भी अपराध करे, तो उसे क्षमा किये जाओ।”
सुवैद बिन मक़रन का बयान है कि हमारे सात भाइयों में एक ग़ुलाम था। एक बार हमारे छोटे भाई ने उसके मुँह पर थप्पड़ मारा तो अल्लाह के रसूल ने हमें आदेश दिया कि हम उसे आज़ाद कर दें।
अरब के लोग ग़ुलाम को अपने साथ जगह देना शर्मनाक समझते थे, लेकिन पैग़म्बर (सल्ल.) ने आदेश दिया कि उन्हें अपने साथ दस्तरख़्वान पर बैठाकर खाना खिलाओ और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक या दो निवाला अपने खाने का उन्हें ज़रूर खिलाओ।
इन सब बातों का उद्देश्य यही था कि दासों को सम्मान और आराम के साथ रखा जाए और वे परिवार के सदस्य के रूप में रहें।
3. इस्लामी क़ानून ने ग़ुलामों को व्यापक अधिकार प्रदान किए जो उन्हें स्वतंत्र लोगों के क़रीब लाते थे, फ़ौजदारी क़ानून उन्हें उन्हीं सुरक्षाओं का अधिकार देता है जिसके हक़दार स्वतंत्र लोग हैं। जो कोई भी उनकी संपत्ति चुराता है, उन्हें मारता है, उनकी महिलाओं से बदसुलूकी करता है, उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाता है, चाहे वह स्वतंत्र हो या ग़ुलाम, किसी भी मामले में उसी सज़ा से दंडित किया जाएगा, जो स्वतंत्र लोगों के ख़िलाफ़ इन अपराधों को करने वाले के लिए निर्धारित है। इसी तरह, नागरिक क़ानून उनकी संपत्ति पर उनके स्वामित्व के अधिकार को मान्यता देता है और उन्हें अपनी निजी संपत्ति का व्यापक अधिकार देता है। क़ानून के अनुसार, उनके स्वामी को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने या उन्हें कोई शारीरिक नुक़सान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। (अनुशासनात्मक कार्रवाईयों को छोड़कर, जिसमें भी शालीनता और सज्जनता पर ज़ोर दिया गया है।)
इस्लामी समाज ने क़ानून से ज़्यादा उन्हें व्यवहार में बराबरी का दर्जा दिया है। सामूहिक जीवन में ग़ुलामों का दर्जा किसी भी तरह स्वतंत्र नागरिक से कम नहीं था। ज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज, हर क्षेत्र में उनके लिए विकास के सभी रास्ते खुले हुए थे और ग़ुलाम होना या न होना उनके लिए किसी भी तरह से बाधक नहीं था। अल्लाह के रसूल ने ख़ुद आपनी फुफेरी बहन सय्यिदा ज़ैनब की शादी अपने मुक्त किए दास ज़ैद बिन हरिसा से कराई थी। इमाम हुसैन की शादी एक ईरानी राजकुमारी से हुई थी जो युद्ध में दासी बनकर आई थी, इमाम ज़ैनुल-अबिदीन उसी दासी की कोख से थे, जो इस्लाम के रईसों में सर्वोच्च दर्जा रखते हैं। इकरामा, जो क़ुरआन के आरंभिक व्याख्याकर्ताओं में से है, स्वयं एक ग़ुलाम थे।
सलमान फ़ारसी ग़ुलाम थे जिन्हें हज़रत अली कहते हैं कि “सलमान, हम अह्ले बैत में से हैं।” बिलाल हब्शी एक ग़ुलाम थे जिन्हें हज़रत उमर कहा करते थे, “बिलाल हमारे आक़ा का ग़ुलाम और हमारा आक़ा है।”
ये शुरुआती शताब्दियों की बातें हैं। बाद में इस्लामी भावना बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शम्सुद्दीन अलतमश और ग़यासुद्दीन बलबन जैसे महान ग़ुलामों ने हमारे देश भारत पर शासन किया है। महमूद ग़ज़नवी, जो अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा विजेता था, वंश के आधार पर तुर्की ग़ुलाम था। मिस्र पर कई शताब्दियों तक ममलुकों का शासन था और उनके नाम से पता चलता है कि वे वास्तव में ग़ुलाम थे जो राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी हुए।
इन ग़ुलामों को कौन ग़ुलाम कह सकता है? क्या आज़ाद नागरिकों को उनसे अधिक उन्नति, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के अवसर मिले थे? क्या उनकी ग़ुलामी ने उन्हें सामाजिक जीवन में ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंचने से रोका? अगर ग़ुलामी इसी चीज़ का नाम है और वह ऐसी ही होती है तो आज़ादी का नाम ग़ुलामी रख देने में क्या हर्ज है?
ये वे तरीक़े थे जिनसे इस्लाम ने ग़ुलामी के धटाते-घटाते आज़ादी से मिला दिया, बल्कि दोनों में कोई अंतर नहीं रहने दिया।'ग़ुलामी' शब्द ज़रूर बना रहा, लेकिन ग़ुलामी की वास्तविकता बदल कर कुछ से कुछ हो गई।
युद्ध की लूट का मामला
इस्लाम में लूट का औचित्य भी उन मुद्दों में से एक है जिस पर विरोधियों ने बहुत टिप्पणियां की हैं और सहयोगियों ने भी इसकी अक्सर ग़लत वकालत की है। तथ्य यह है कि इस्लाम ने लूट के मामले में भी धीरे-धीरे सुधार का वही तरीक़ा अपनाया है जो ग़ुलामी के मामले में अपनाया गया था। अरब में लूट की लालसा किस हद तक बढ़ी हुई थी, उसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। लूट का माल प्राप्त करना वह सबसे बड़ा प्रेरक था जिसके लिए एक अरब युद्ध के ख़तरों को सहन करने और मारने-मरने को तैयार रहता था। अरब युद्ध के अर्थ में ही लूटपाट शामिल था, युद्ध शब्द की अवधारणा भी मन में तब तक पूरी नहीं हो सकती थी, जब तक उसमें लूटपाट का अर्थ शामिल न हो।
जब इस्लाम आया तो अरबों ने इसी निहित आकर्षण के साथ उसमें प्रवेश किया। सदियों से विरासत में मिली मानसिकता को एक़दम बदल देना नामुमकिन था। जिन नव-मुस्लिम अरबों को सुधारना था, उनकी स्थिति यह थी कि अनायास उनका खिंचाव दुश्मन के माल की ओर होता था, युद्धभुमि में माल देखने के बाद वे अपने आप पर नियंत्रण खो देते थे। बद्र की लड़ाई से पहले, पैगंबर (सल्ल.) ने दुश्मन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अब्दुल्लाह बिन जहश को एक दल के साथ बतन नखला की ओर भेजा था। रास्ते में कुछ कुरैशी व्यापारियों से उनकी मुठभेड़ हुई, दुश्मन का माल देखकर उनके आदमी नियंत्रण से बाहर हो गए और व्यापारियों को मार कर उनका माल लूट लिया। इतिहासकारों ने इस घटना को बद्र की लड़ाई के तात्कालिक कारणों में से एक माना है।
बद्र की लड़ाई में ही एक ओर सीरिया से क़ुरैश का व्यापार कारवाँ आ रहा था और दूसरी ओर मक्का से क़ुरैश के सैनिक आ रहे थे, हालाँकि उस समय दुश्मन की ताक़त को तोड़ना सबसे ज़रूरी था, लेकिन इस्लामी सेना की सामान्य इच्छा यही थी कि पहले उसके काफिले पर हमला करके लूटपाट की जाए। कुरान में इसका उल्लेख है:
وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَـٰفِرِينَ○ (الانفال ۷)
“और जब अल्लाह वादा कर रहा था कि तुम दोनों गिरोहों में से किसी एक गिरोह पर हावी हो जाओगे और तुम चाहते थे कि कमज़ोर और निहत्थे गिरोह तुम्हारे हाथ लग जाए, हालाँकि अल्लाह चाहता था कि वह अपनी बातों से सत्य को सत्य कर दिखाए और अवज्ञाकारियों की जड़ काट दे।” (अल-अनफ़ाल: 7)
फिर जब युद्ध जीत लिया गया, तो सहाबियों के पवित्र समूह के लिए लूट की चाहत को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और वे अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना लूटपाट में लगे रहे। उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई:
لَّوْلَا كِتَـٰبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ○ (الانفال :۶۸)
“अगर पहले से अल्लाह का लिखित आदेश न आ गया होता, तो तुमने जो किया है, उस की बहुत बड़ी सज़ा मिली होती।” (अल-अनफ़ाल: 68)
उहुद की लड़ाई में लूट की इसी चाहत ने जीत को हार में बदल दिया। जैसे ही क़ुरैश के पाँव हटे, सहाबा लूट की तरफ़ मुड़े और उन तीरंदाज़ों को भी अल्लाह के रसूल के उस आदेश की याद न रही जिस को उन्होंने पीछे से होने वाले हमले से बचाव के लिए खड़ा किया था, नतीजा यह हुआ कि इस्लामी सेना तितर-बितर हो गई और अवज्ञाकारियों की सेना ने पलटकर ऐसा आक्रमण किया कि अल्लाह के रसूल स्वयं घायल हो गए। हुनैन में भी ऐसा ही हुआ कि पहले आक्रमण में ही शत्रु असंगठित हो गये, इस्लाम में नये आमे वाले अरब लूट के माल पर टूट पड़े। फिर उनका ध्यान दूसरी ओर देखकर बनी हवाज़िन के धनुर्धारियों ने ऐसा आक्रमण किया कि बड़े-बड़े बहादुरों के पांव उखड़ गए।
इन घटनाओं का वर्णन करने का उद्देश्य सहाबियों को बदनाम करना नहीं है, बल्कि केवल यह कहना है कि लूट की चाहत एक स्वभाविक भावना थी, जो सदियों की परंपराओं से इतनी जड़ पकड़ गई थी कि कोई मानव समूह यहां तक कि अल्लाह के रसूल के सहाबियों का दल भी इससे बचा हुआ नहीं था। जब स्थिति यह थी तो एक बुद्धिसम्मत धर्म, जो प्रकृति से लड़ना नहीं चाहता था बल्कि उसे सुधारना चाहता था, इस से बेहतर क्या तरीक़ा अपना सकता था कि शत्रु सम्पत्ति को वैध ठहरा देता और अप्रत्यक्ष तरीक़ों से उसकी चाहत को कम करने की कोशिश करता। इस्लाम ने यही रास्ता अपनाया। शत्रु सम्पत्ति को वैध बनाने का कारण एक हदीस से पता चलता है जिसे इमाम यूसुफ़ ने हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से उद्धृत किया है:
“अल्लाह के रसूल, ने कहा कि तुमसे पहले किसी काले सिर वाले लोगों के लिए शत्रु सम्पत्ति को वैध नहीं बनाया गया था। एक आग आसमान से उतरती थी और उस माल को भस्म कर देती थी। जब बद्र की लड़ाई हुई, तो लोग शत्रु सम्पत्ति पर टूट पड़े। उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अगर अल्लाह का लिखित आदेश पहले न आ चुका होता, तो तुम पर बड़ी यातना आ जाती, इसलिए अब जो कुछ तुमने लूटा है उसे खाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हलाल और पाक है।
इस हदीस से मालूम होता है कि शत्रु सम्पत्ति पहले हलाल नहीं थी, लेकिन इंसानी फितरत की न बदलने वाले रुझान को देखते हुए उसे हलाल कर दिया गया। हालाँकि, उस प्रवृत्ति को ठीक करने और सीमित करने के लिए कई तरीक़े अपनाए गए, जिसने धीरे-धीरे दिलों से शत्रु सम्पत्ति की चाहत को कम कर दिया। जो कुछ रह गया, उसे इस तरह से सुधारा गया कि शत्रु सम्पत्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए और उस का दायरा भी बहुत सीमित कर दिया गया।
इस संबंध में विशेष रूप से तीन विधियां उल्लेखनीय हैं:
(1) इस्लाम ने शत्रु सम्पत्ति के मूल्य को इस हद तक गिरा दिया कि धार्मिक लोगों में अब इसे हासिल करने की इच्छा ही नहीं रह गई। सबसे पहले कहा गया कि जो व्यक्ति लूट के इरादे से लड़ेगा उसे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, इनाम केवल उनके लिए है जो अपने दिलों को सांसारिक लक्ष्यों से मुक्त रखते हैं और अल्लाह की खातिर लड़ते हैं। फिर जब लूट से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने का मूल्य दिलों में पैदा कर दिया गया, तो कहा गया कि जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने युद्ध का लाभ प्राप्त करता है, उसके लिए आख़िरत का इनाम कम हो जाएगा, और जो दुनिया में फ़ायदा नहीं लेगा, उसे आख़िरत में पूरा इनाम मिलेगा।
“जिस सेना ने अल्लाह के मार्ग में लड़ाई की और शत्रु सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा कर लिया, उसने अपने आख़िरत के इनाम में से दो-तिहाई यहीं पा लिया, अब आख़िरत में उसके लिए केवल एक तिहाई रहेगा, और जिसने लूट पर क़ब्ज़ा नहीं किया, वह उसका इनाम प्राप्त करेगा।”
इस शिक्षा ने मुसलमानों में शत्रु सम्पत्ति की इच्छा से अधिक परलोक के प्रतिफल की इच्छा पैदा कर दी और वही अरब जो शत्रु सम्पत्ति के ढेर देखकर बेक़ाबू हो जाया करते थे, कुछ ही वर्षों में सांसारिक संपत्ति के प्रति इतने उदासीन हो गए कि उन्हें वह पेश की गई और उन्होंने मना कर दिया। पैग़म्बर (सल्ल.) के जीवन के आखिरी दौर में जब तबुक की लड़ाई के लिए आम घोषणा की गई, तब वासिला बिन असक़अ ने लोगों से कहा कि जो भी मुझे अपने साथ लड़ाई में ले जाएगा, मैं उसे शत्रु सम्पत्ति का आधा हिस्सा दूंगा। अंसार के एक सहाबी ने इस शर्त को स्वीकार किया और उसे अपने साथ ले गए। युद्ध में इस्लामी सेना को जो शत्रु सम्पत्ति मिली थी, उसमें से कुछ बहुत अच्छे युवा ऊँट वासिला के हिस्से में आए थे, जिन्हें वे उन अंसारी सहाबी के पास ले गए और कहा कि यह है वह माल। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मेरा उद्देश्य लूट हासिल करना नहीं है, बल्कि केवल आखिरत के इनाम की चाहत थी।
एक बार एक बैडोइन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ जिहाद में शरीक हुआ। युद्ध में कुछ शत्रु सम्पत्ति हाथ आई तो पैग़म्बर (सल्ल.) सब की तरह उस बैडोइन का भी हिस्सा लगाया। जब उसे ख़बर मिली तो वह सामने आया और कहने लगा, “मैंने इस माल के लिए आपका साथ नहीं दिया, मैं तो चाहता हूं कि इस जगह (कंठ की ओर संकेत करके) तीर खाऊं और शहीद हो जाऊं।” (निसाई)
2 शत्रु सम्पत्ति में, ज़रूरतमंदों, विकलांगों और ग़रीबों के भरण-पोषण के लिए और सामान्य राष्ट्रीय ज़रूरतों के लिए पाँचवाँ भाग निर्धारित किया गया:
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ○(الانفال :۴۱)
“और जान लो कि तुम्हें जो कुछ शत्रु सम्पत्ति के रूप में मिला है, उसका पाँचवाँ भाग अल्लाह तथा रसूल और (उनके) समीपवर्तियों तथा अनाथों, निर्धनों और यात्रियों के लिए है।” (अल-अनफ़ाल :41)
इस पद्धति से, शत्रु सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा भलाई के कामों के लिए अलग रखा जाता था, इस तरह सेना के हिस्से में बहुत कमी आ गई।
शत्रु सम्पत्ति पहले हर उस संपत्ति को कहा जाता था, जिसे सेना दुश्मन के देश से लूटती थी, चाहे वह किसी भी तरह लूटी गई हो, लेकिन इस्लाम केवल उस संपत्ति को शत्रु सम्पत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना से विजयी सेना के हाथ आए। इस तरह एक ओर, शांतिपूर्ण ग़ैर-सैन्य आबादी में सेना द्वारा सामान्य लूटपाट को शत्रु सम्पत्ति की वैध सीमा से बाहर रखा गया, दूसरी ओर, वह माल भी शत्रु सम्पत्ति की परिभाषा से बाहर हो गया है जो युद्ध के बिना मुसलमानों के हाथ आता है, या जिस पर युद्ध के अंत के बाद इस्लामी सेना द्वारा क़ब्ज़ा कर लिया जाता है।
साथ ही इस परिभाषा के अनुसार वे सभी संपत्तियां भी शत्रु सम्पत्ति की परिभाषा से बाहर हो जाती हैं, जो सामरिक कार्रवाइयों के फलस्वरूप शत्रु देश से निकलकर इस्लामी राज्य के अधिकार में आ जाती हैं। इस्लाम ने उस माल को सेना में विभाजित करने के बजाय इस्लामी राज्य के स्वामित्व में दिया है। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है:
وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍۢ وَلَا رِكَابٍۢ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ○ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ○ (الحشر :۶-۷)
“और जो फ़य का धन अल्लाह ने अपने रसूल को दिला दिया उसपर, तुमने अपने घोड़े और ऊँट नहीं दौड़ाये, बल्कि अल्लाह अपने रसूल को, जिसपर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है तथा अल्लाह जो चाहे, कर सकता है। तो ऐसा धन जो अल्लाह अपने रसूल को फ़य के रूप में दिलवाए, वह अल्लाह, उसके रसूल, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों तथा यात्रियों के लिए है; ताकि वह (धन) तुम्हारे धनवानों के बीच ही फिरता न रह जाए।” ( अल-हश्र: 6-7)
इस आयत से यह स्पष्ट हो गया है कि सेना द्वारा अपने घोड़ों और ऊँटों को दौड़ाकर (अर्थात् युद्ध के मैदान में लड़कर) जो धन प्राप्त किया जाता है, वही शत्रु संपत्ति की परिभाषा में आती है। जो सम्पत्ति युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम न हों, तो वे इस्लामी राज्य और ख़ुदा और रसूल के कामों में ख़र्च होने के लिए है।
इस आदेश पर जब बाद में पैग़म्बर (सल्ल.) के साथियों ने विचार किया, तो यह देखा गया कि फ़य के पात्रों में छह नाम छ: नाम गिनाए गए हैं- “अल्लाह, रसूल, रसूल के क़रीबी, अनाथ, अभावग्रस्त, और यात्री। इनमें से केवल एक, ‘रसूल’ इस दुनिया को छोड़कर चले गये हैं, शेष सभी हमेशा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, “इन छ: अधिकार धारकों का अधिकार” घोषित करने की समीचीनता यह थी कि यह धन अकेले अमीरों में नहीं घूमता फिरे, बल्कि राष्ट्र के सभी वर्गों को इससे लाभ पहुंचे। इस आधार पर यह क़ानून बनाया गया है कि “फ़य” के धन को अल्लाह और रसूल के कामों और उम्मत के सामान्य वर्गों की सेवा के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
इसी क़ानून के अनुसार, हज़रत उमर ने विजित देशों को सेना में बांटने से इनकार कर दिया और सेना को केवल उस धन पर संतोष करना पड़ा जो युद्ध के दौरान दुश्मन सेना से प्राप्त कर लिया गया था। इस संबंध में हज़रत उमर का वह पत्र जो उन्होंने साद बिन अबी वक़्क़ास को लिखा था, इस्लामी क़ानून को बहुत स्पष्ट करता है। बिलाज़िरी ने इस पत्र को इन शब्दों में उद्धृत किया है:
“तुम्हारा पत्र आया। तुम लिखते हो कि लोग तुमसे कह रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें शत्रु सम्पत्ति के रूप में जो कुछ दिया है, उसे विभाजित कर दिया जाए। इसलिए, मेरा पत्र प्राप्त करने के बाद, ऐसा करो कि सेना ने अपने घोड़ों और ऊंटों को दौड़कर जो संपत्ति और जानवर लूटे हैं, उनका पांचवां भाग निकालने के बाद, शेष को सिपाहियों में बांट दो। शेष ज़मानों और नदियों को किसानों के पास रहने दो ताकि मुसलमानों के वेतन के काम आएं। अगर उन्हें भी वर्तमान युग के लोगों में बांट दोगे तो बाद में आने वालों के लिये कुछ न बचेगा।”
इस प्रकार, इस्लाम ने एक ओर शत्रु सम्पत्ति की इच्छा को कम कर दिया, जो कि लूटपाट और हिंसा का मुख्य प्रेरक था, दूसरी ओर, इसने ऐसे क़ानून बनाए जो शत्रु सम्पत्ति के दायरे को केवल उन संपत्तियों तक सीमित कर देते थे जो युद्ध के दौरान प्राप्त कर ली गई हो। तीसरे इस शत्रु सम्पत्ति का पाँचवाँ भाग भलाई के कार्यों के लिए अलग कर लिया। अब, जिसे इस्लामी शब्दावली में ‘ग़नीमत’ शब्द से संदर्भित किया जाता है, (और जिसका हिन्दी अनुवाद इस किताब में ‘शत्रु सम्पत्ति’ और ‘विजयधन’ लिखा गया है) ठीक वही है जिसे पश्चिमी क़ानून में ‘युद्ध की लूट’ Spoils of war कहा जाता है और जिसे दुनिया के सभी विधिवेत्ताओं द्वारा विजेता के प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर केवल इतना है कि पश्चिमी क़ानून उस पूरी लूट को राज्य का हिस्सा ठहराता है और इस्लामी क़ानून इसका पांचवां हिस्सा लेकर शेष चार भागों को बहादुर सैनिकों में वितरित कर देता है जिन्होंने अपना ख़ून बहाकर उन्हें प्राप्त किया है।
संघर्षविराम और शरण
इस्लामी युद्ध के संस्कारों में से एक यह है कि एक मुसलमान को हमेशा सुलह के लिए तैयार रहना चाहिए। चूंकि इस्लामी युद्ध का लक्ष्य “युद्ध” नहीं है बल्कि सुधार, शांति और सुरक्षा है, अगर सुलह के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई अवसर है, तो हथियार उठाने से पहले इसका लाभ उठाना चाहिए। इस्लाम ने युद्ध की अंतिम सीमा शांति को ठहराया है। पवित्र क़ुरआन हमें आदेश देता है कि अगर दुश्मन तुमसे शांति मांगता है, तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो:
وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (انفال: ۶۱ - ۶۲)
“अगर वे शांति के लिए झुकते हैं, तो तुम भी झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो कि वह सब कुछ सुनता और जानता है। और अगर वे तुम्हें धोखा देना चाहें, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही है जिसने तुम्हें सहारा दिया और ईमानवालों की संख्या से तुम्हें मज़बूत किया है।” (अल-अनफ़ाल :61-62)
यह भी आदेश है कि अगर कोई दुश्मन हथियार डाल दे और बोलकर या बिना कहे सुलह मांगे तो तुमको उस पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं रह जाता।
فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًۭا○ (النساء :۹۰)
“फिर अगर वे तुम से हाथ खींच लें, युद्ध न करें, और शान्ति की इच्छा करें, तो ऐसी हालत में अल्लाह ने उनके विरुद्ध तुम्हे हाथ उठाने का अधिकार नहीं दिया है।” (अल-निसा': 90)
इसी तरह, अगर दुश्मन राष्ट्र के सदस्य मिल जाएं और शांति की मांग करें, तो उन्हें मारना जायज़ नहीं है, बल्कि उन्हें शांति के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और जब वे अपने देश लौटना चाहें, तो उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए:
وَإِنْ أَحَدٌۭ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَعْلَمُونَ○ (التوبہ : ۶)
“अगर मुशरिकों में से कोई तुम्हारी पनाह मांगे, तो उसे पनाह दो, यहां तक कि वह अल्लाह की वाणि सुन ले, फिर उसे उसकी शांति की जगह तक पहुंचा दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं।” (अल-तौबा :6)
पराजित राष्ट्रों के साथ मामला
युद्ध का विषय पूरा हुआ। अब हमें युद्ध से जुड़े विषयों पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। दुश्मन के साथ ऐसी स्थिति में सद्व्यवहार करना कि उसके पास प्रतिरोध की शक्ति मौजूद हो, किसी हद तक एक रणनीति कही जा सकती है। लेकिन जब उसकी प्रतिरोध की शक्ति पूरी तरह से टूट जाए और वह अपने आप को विजेता की दया पर छोड़ दे, तो उसके साथ उदारता का व्यवहार करना शुद्ध और पूर्ण अच्छाई है, जो विजेता के अच्छे इरादों को पूरी तरह स्पष्ट करता है। पराजित के प्रति विजेता का व्यवहार वास्तव में विजेता की जीत के लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर उसने धन के लिए विजय प्राप्त की है, तो उसकी राजनीती में शोषण हावी होगा। अगर यह धार्मिक शत्रुता पर आधारित है, तो शासन में धार्मिक पूर्वाग्रह और हिंसा प्रमुख होगी। अगर साम्राज्य विस्तार और वर्चस्व का लोभ उसकी प्रेरणा रहा है तो प्रशासन का सारा तंत्र ही दमन और अहंकार पर आधारित होगा। इसके विपरीत, अगर विजेता का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि वास्तविक सुधार और कल्याण है, तो वह पराजित राष्ट्र की न संपत्ति लूटेगा, न धार्मिक हिंसा फैलाएगा, न क्रूरता का व्यवहार करेगा और न उसे अपमानित करके उसे अपना ग़ुलाम बनाएगा, बल्कि उनका शासन न्याय, सहिष्णुता, समानता और उदारता पर आधारित होगा। उनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत विजित राष्ट्र को बिगाड़ और उपद्रव से रोकना और शांति से नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करना होगा। अब, इस मानक के अनुसार, हमें यह देखना चाहिए कि इस्लाम अपने पराजित राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसका क़ानून पराजितों को क्या दर्जा देता है? उसकी शरीयत उनके लिए क्या अधिकार निर्धारित करती है? और उसकी सरकार उनके साथ भलाई का व्यवहार करती है या बुराई का?
दो प्रकार के पराजित
इस्लामी क़ानून ने सभी पराजितों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक वे हैं जो शांति के साथ आज्ञाकारिता स्वीकार करते हैं, दूसरे वे हैं जो तलवार के बल पर पराजित किए गए हैं। दोनों के मामलों में थोड़ा सा अंतर है, तो हम दोनों के मामलों को अलग-अलग बयान करेंगे:
संधि राज्य
जो लोग युद्ध से पहले या उसके दौरान अधीनता स्वीकार कर लें और इस्लामी शासन के साथ विशिष्ट शर्तें तय कर लें उनके लिए इस्लाम का क़ानून यह है कि उनके साथ सभी व्यवहार समझौते की उन शर्तों के अधीन होंगे जिन पर वे सहमत हुए हैं। दुश्मन को प्रेरित करने के लिए कुछ शर्तों को तय कर लेना और फिर जब वे पूरी तरह से नियंत्रण में आजाए तो उसके साथ अलग व्यवहार करना, यह आधुनिक सभ्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रथाओं में से एक है। लेकिन इस्लाम इसे नाजायज़, वल्कि हराम मानता है और वह इसे एक बड़ा गुनाह ठहराता है। उसके अनुसार, यह ज़रूरी है कि जब किसी राष्ट्र के साथ कुछ शर्तों पर सहमति हो जाए, चाहे वे वांछनीय हों या न हों, तो उन शर्तों का एक अंश भी उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) कहते हैं:
“अगर तुम किसी राष्ट्र से लड़ते हो और उस पर विजय प्राप्त करते हो, और वह राष्ट्र अपनी और अपनी संतान की जान बचाने के लिए तुमको लगान देने पर सहमत हो जाए (एक संधि कर ले), तो तुम उस निर्धारित लगान से एक दाना भी ज़्यादा मत लेना क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।” (अबू दाऊद, किताबुल-जिहाद)
एक अन्य हदीस में है:
“ख़बरदार! जो कोई किसी संधि राष्ट्र पर अत्याचार करेगा, उसके अधिकारों को कम करेगा या उस पर उसकी ताक़त से अधिक बोझ डालेगा या उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कुछ लेगा, तो क़ियामत के दिन मैं ख़ुद उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा करूंगा।” (अबू दाऊद, किताबुल-जिहाद)
इन दोनों हदीसों के शब्द सामान्य हैं और उनसे यह सामान्य नियम निकलता है कि ज़िम्मियों के साथ जिन शर्तों पर समझौता हो जाए, उनमें कोई कमी या वृद्धि करना जायज़ नहीं है। न उनके करों में वृद्धि की जा सकती है, न उनकी भूमि को ज़ब्त किया जा सकता है, न उनकी इमारतें छीनी जा सकती हैं, न उन पर गंभीर आपराधिक क़ानून लागू किए जा सकते हैं, न उनके धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है, न ही उनके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला किया जा सकता है और न ऐसा कोई कार्य किया जा सकता है, जो क्रूर या अपमानजनक हो। इन फ़ैसलों के आधार पर, इस्लामी न्यायविदों ने शांति से जीते गए राष्ट्रों के बारे में किसी भी तरह का क़ानून नहीं बनाया और केवल सामान्य नियम बताकर छोड़ दिया कि उनके साथ हमारा व्यवहार शांति की शर्तों के अनुसार होगा।
यह स्पष्ट है कि समझौता ज्ञापन के लिए नियम और विनियम निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। समय और अवसर के आधार पर जो उपयुक्त हो, निर्धारित की जाएंगी। पैग़म्बर (सल्ल.) और उनके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो समझौते किए हैं, उनसे हमें उन सामान्य सिद्धांतों की जानकारी मिलती है जिनके आधार पर इस्लाम अपने दुश्मनों के साथ समझौता कर सकता है। उन सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए, हम यहां कुछ समझौतों को उद्धृत कर रहे हैं:
नजरान के लोगों के अनुरोध पर, पैग़म्बर (सल्ल.) ने जो संधि लिखकर उन्हें दी थी, उसमें लिखा था:
“नजरान के ईसाइयों और उनके पड़ोसियों के लिए, अल्लाह की शरण और अल्लाह के दूत मुहम्मद की ज़िम्मेदारी है, उनके जीवन, उनके धर्म, उनकी भूमि, उनकी संपत्ति, उनके उपस्थित और अनुपस्थित, उनके ऊंटों, उनके संदेशवाहक और उनके धार्मिक संकेतों, सभी के लिए। वे अब तक जिस स्थिति में हैं, उसी पर बहाल रहेंगे। उनके अधिकारों में से कोई अधिकार और और संकेतों में से कोई संकेत भी नहीं बदला जाएगा। उनके किसी बिशप को, संन्यासी को, गिरजाधर के सेवक को, उनके पद और उनकी सेवा से नहीं हटाया जाएगा, चाहे उसके हाथ के नीचे जो कुछ है, वह कम हो या ज़्यादा। इन पर इस्लामपूर्व अरब के किसी ख़ून या वचन का कोई दायित्व नहीं है। उन्हें सैन्य सेवा या किसी भी बल का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और कोई भी सेना उनकी भूमि को नहीं रौंदेगी। अगर कोई व्यक्ति उनके ख़िलाफ़ किसी भी अधिकार का दावा करेगा, तो पक्षों के बीच न्याय किया जाएगा। नजरान के लोग न तो अत्याचारी बन सकेंगे और न ही पीड़ित। लेकिन जिसने इसके पहले सूद लिया है, मैं उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी से मुक्त हूं। उनमें से किसी को भी दूसरे के गुनाह में नहीं पकड़ा जाएगा। इस लेख में जो कुछ है उसके लिए अल्लाह की ज़मानत और मुहम्मद पैग़म्बर (सल्ल.) का ज़िम्मा है, हमेशा के लिए, जब तक अल्लाह का आदेश आए और जब तक वे शुभचिंतक रहें, और उन दायित्वों को पूरा करते हैं जो इस समझौते के आधार पर उन पर लगाए गए हैं।”
हज़रत अबू बक्र के समय में ख़ालिद बिन वलीद ने हैरा के लोगों के लिए एक शांति संधि लिखी थी, उस में उन्होंने प्रति व्यक्ति केवल 10 दिरहम लगान लगाया था। (ग़रीबों और अक्षम लोगों को छोड़ कर) इस्लामी राज्य की ओर से यह प्रतिज्ञा की गई कि:
“उनका कोई उपासनागृह नहीं तोड़ा जाएगा, न कोई किला, जिसमें वे अपने शत्रुओं से बचाव के लिए शरण लेते हैं, नष्ट नहीं किया जाएगा, न उन्हें घंटा (शंख) बजाने से रोका जाएगा, न उन्हें अपने त्योहार के दिन क्रास निकालने से मना किया जाएगा।”
हज़रत उमर ने बैतुल मक़दिस के लोगों को जो शांति संधि लिखकर दी थी, उसके शब्द ये हैं:
“उन्हें अमान दी उनके जीवन की उनके धन की, उनके चर्चों और उनके क्रास की, उनके स्वस्थ और बीमारों के लिए, यह शान्ति एलिय्याह के सारे समुदाय के लिये है। यह वादा किया गया है कि उनके आराधनालय को मुसलमानों का निवास नहीं बनाया जाएगा। न तो उन्हें तोड़ा जाएगा और न ही उनके परिसरों और भवनों में कोई कमी की जाएगी। न तो उनके क्रॉस और न ही उनकी किसी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया जाएगा, न ही धर्म के मामलों में उन पर कोई दबाव डाला जाएगा और न ही उनमें से किसी को नुक़सान पहुंचाया जाएगा।”
इस्लामी शासनकाल में इस तरह के अनगिनत समझौते मौजूद हैं। हमने विशेष रूप से उन समझौतों को उद्धृत किया है, जो पैग़म्बर (सल्ल.) और उनके साथियों ने तब किए थे जब वे पूरी तरह से प्रबल हो गए थे। नजरान की सन्धि उस समय हुई जब इस्लाम की धाक पूरे अरब पर बौठ गई थी और नजरान के लोगों ने स्वयं भयभीत होकर अपने नेतृत्व को सुलह के लिए भेजा था। हैरा की सन्धि तब संपन्न हुई जब आसपास के स्थानों पर ख़ालिद बिन वलीद विजय प्राप्त कर चुके थे, और हैरा के लोगों ने इसमें अपना भला देखा था कि स्वयं आगे बढ़कर आज्ञाकारिता स्वीकार कर लें। दमिश्क और यरूशलेम के बारे में, आप पहले से ही जानते हैं कि वे लगभग जीते जा चुके थे। और अगर मुसलमान उन्हें तलवार से जीतना चाहते तो उनके लिए यह मुश्किल नहीं था। ऐसे में शांति संधि करना और उन शर्तों पर करना जो ऊपर उल्लिखित हैं, उस राष्ट्र का कार्य नहीं हो सकता था जिसका उद्देश्य बलपूर्वक अपने धर्म का प्रसार करना हो, या जिसने दूसरे धर्मों को मिटा देने के लिए तलवार उठाई हो या जो केवल लूटपाट और साम्राज्य विस्तार के लिए निकला हो।
ग़ैर-संधि वाले राज्य
विजितों की दूसरी श्रेणी में वे हैं जिन्होंने अंत तक मुसलमानों से लड़ाई लड़ी और जिन्होंने तब आत्मसमर्पण किया हो, जब इस्लामी सेनाएँ उनकी क़िलेबंदी को तोड़कर उनकी बस्तियों में विजयी रूप से प्रवेश कर गईं। ऐसे पराजितों के बारे में इस्लाम ने विजयी राष्ट्र के इस अधिकार को मान्यता दी है, कि अगर वह चाहे तो उनके हथियार उठाने वाले सभी पुरुषों को मार डाले, उनकी महिलाओं और बच्चों को ग़ुलाम बनाले और उनकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर ले। लेकिन पहला तरीक़ा यह है कि उन्हें भी ज़िम्मी बना दिया जाए और उन्हें उनके घरों में उसी स्थिति में रहने दिया जाए, जो युद्ध के पूर्व थी। आप जानते हैं कि उस समय का सामान्य चलन यही था कि पराजितों को ग़ुलाम बना लेते, उनकी संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर लेते और शहरों को जीतने के बाद नरसंहार करके उनकी युद्ध शक्ति को नष्ट कर देते थे। इस्लाम के लिए इस सामान्य मानसिकता को बदलना मुश्किल था। युग की भावना से लड़ना उसके सुधार के तरीक़े के ख़िलाफ़ था। इसलिए उसने एक ओर परंपराओं और रीति-रिवाजों से प्रभावित मन को संतुष्ट करने के लिए पिछले तरीक़े को शाब्दिक रूप में बनाए रखा और दूसरी ओर अल्लाह के रसूल और उनके साथियों ने अपने मार्गदर्शन से मुसलमानों के बीच इतनी उदारता की भावना पैदा कर दी कि वे स्वयं इस अनुमति का लाभ उठाना पसंद नहीं करते थे, और धीरे-धीरे एक दूसरी प्रति-प्रथा उठी जिसने व्यावहारिक रूप से पिछली प्रथा को निरस्त कर दिया। नबुव्वत के दौर और सही ख़लीफ़ाओं के दौर का इतिहास, बल्कि पूरे इस्लामी दौर का इतिहास भी बताता है कि मुसलमानों ने हज़ारों देशों और शहरों को जीता, लेकिन उनमें से किसी एक में भी न नरसंहार किया, न निवासियों को ग़ुलाम बनाया और न ही उनकी संपत्ति को ज़ब्त किया। ( बनी क़ुरैज़ा का मामला इसका अपवाद है और इस पर विस्तृत चर्चा होगी।)
पैग़म्बर (सल्ल.) के समय में ख़ैबर पर विजय प्राप्त की गई तो नबी ने इसके निवासियों को ज़िम्मी बना लिया। मक्का पर जीता गया, लेकिन न भूमि को सेना के बीच विभाजित किया गया था और न निवासियों को ग़ुलाम बनाया गया। हुनैन की लड़ाई में हवाज़िन की हार हुई और पैग़म्बर (सल्ल.) के आदेश से उसकी जान बख्श दी गई। हज़रत उमर के समय में, जब इराक़ और सीरिया के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी, तो पहली बार इस्लामी सेना में जीत का फ़ायदा उठाने और भूमि को विभाजित करने और निवासियों को ग़ुलामों के रूप में लेने की भावना पैदा हुई, इसलिए उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि “हमने अपने ख़ून से ज़मीन को जीता है, इसलिए इसे हमारे बीच बांट दिया जाए और इसके निवासियों को ग़ुलाम बना लिया जाए।” लेकिन हज़रत उमर ने अपने शक्तिशाली तर्कों से उनका दिल बदल दिया और वह प्राचीन मानसिकता हमेशा के लिए बदल गई।
मुसलमानों को विजित शहरों के पूजा स्थलों पर क़ब्ज़ा करने का अधिकार है, लेकिन यह बेहतर है कि इस अधिकार का उपयोग न किया जाए और उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए जैसे वे हैं। हज़रत उमर के समय जितने भी देशों पर विजय प्राप्त की गई, उनमें से किसी के भी पूजा स्थल को नष्ट नहीं किया गया और न ही इन में किसी तरह का हस्तक्षेप किया गया।
ज़िम्मियों (इस्लामी राज्य के ग़ैरमुस्लिम नागरिकों) के सामान्य अधिकार
अब हम ज़िम्मियों के अधिकारों का वर्णन करेंगे जो उन सभी लोगों के लिए सामान्य है, जिनका ज़िम्मा राज्य द्वारा उठाया जाता है, चाहे वे संविदात्मक हों या ग़ैर-संविदात्मक, चाहे उनके साथ शांति समझौता हुआ हो या वे युद्ध करके जीते गए हों।
(1) ज़िम्मी के ख़ून की क़ीमत मुसलमान के ख़ून के बराबर है। अगर कोई मुसलमान किसी ज़िम्मी की हत्या करता है तो उसका बदला उसी तरह लिया जाएगा जैसे किसी मुसलमान की हत्या के मामले में लिया जाता है।
पैग़म्बर (सल्ल.) के समय में, एक मुसलमान ने एक ज़िम्मी को मार डाला, तब पैग़म्बर (सल्ल.) ने उसकी हत्या का आदेश दिया और कहा, “मैं अपने दायित्व को पूरा करने का सबसे अधिक हक़दार हूं!”
हज़रत उमर के समय में बक्र बिन वायल के क़बीले के एक व्यक्ति ने हैरा के एक ज़िम्मी को मार डाला। इसपर उन्होंने आदेश दिया कि हत्यारे को मृतक के उत्तराधिकारियों के कर दिया जाए। फिर वह मृतक के वारिसों को दे दिया गया और उन्होंने उसे मार डाला।
हज़रत अली के समय में एक मुसलमान पर एक ज़िम्मी की हत्या का आरोप लगाया गया। सुबूत पूरा होने के बाद, उन्होंने अपराधी की हत्या का आदेश दिया। मृतक के भाई ने आकर कहा कि मैंने ख़ून माफ़ कर दिया। लेकिन वे संतुष्ट न हुए कहा: “शायद लोगों ने तुम्हें डराया धमकाया है।” उसने जवाब दिया नहीं मुझे हर्जाना मिल गया है। तब उन्होंने हत्यारे को रिहा कर दिया।
(2) ताज़ीरात में ज़िम्मी और मुसलमान का दर्जा समान है। अपराधों की जो सज़ा एक मुसलमान को दी जाएगी वही एक ज़िम्मी को मिलेगी। ज़िम्मी की संपत्ति कोई मुसलमान चुराए या मुसलमान की संपत्ति ज़िम्मी चुराए, दोनों हालतों में चोर का हाथ काट दिया जाएगा। ज़िम्मी किसी मुस्लिम महिला के साथ व्यभिचार करे या मुसलमान किसी ज़िम्मी महिला के साथ व्यभिचार करे, दोनों मामलों में सज़ा समान होगी।
(3) नागरिक क़ानून में भी ज़िम्मी और मुस्लिम के बीच पूर्ण समानता है। हज़रत अली का कथन है कि उनकी संपत्ति की रक्षा उसी तरह होनी चाहिए जैसे मुसलमानों की संपत्ति की। इस अध्याय में ज़िम्मियों के अधिकारों पर इतना ज़ोर दिया गया है कि अगर कोई मुसलमान उनकी शराब या उनके सूअरों को भी नष्ट कर देता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति अनिवार्य़ होगी।
(4) किसी ज़िम्मी को जीभ से या हाथ-पैर से कष्ट पहुँचाना, उसे गाली देना, पीटना या उसकी पीठ-पीछे बुराई करना, उसी तरह नाजायज़ है जिस तरह किसी मुसलमान के लिए नाजाइज़ है।
(5) ज़िम्मा उठाने का क़रार मुसलामानों पर हमेशा के लिए बाध्यकारी होता है यानी मुसलामानों को उसे तोड़ने की आज़ादी नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर, ज़िम्मियों को यह अधिकार है कि वे जब तक चाहें उसपर बने रहें और जब चाहें उसे तोड़ दें।
(6) ज़िम्मी चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं टूटती। यहां तक कि जिज़्या रोकना, किसी मुसलमान की हत्या, पैग़म्बर (सल्ल.) का अपमान करना, या मुस्लिम महिला का बलात्कार करना भी उसके ज़िम्मे को नहीं तोड़ता। केवल दो स्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें ज़िम्मेदारी का अनुबंध बाक़ी नहीं रहता है, एक यह कि वह दारुल-इस्लाम को छोड़ दे और दुश्मनों से जा मिले, और दूसरा यह है कि वह इस्लामी राज्य के ख़िलाफ़ खुले तौर पर विद्रोह कर दे।
(7) ज़िम्मियों के व्यक्तिगत मामले उनके पर्सनल लॉ के अनुसार तय किए जाएंगे, उन पर इस्लामी क़ानून नहीं थोपा जाएगा। जो गतिविधियां उनके लिए जायज़ हैं चाहे वे इस्लाम में निषिद्ध ही क्यों न हों, उन्हें वे अपनी बस्तियों में कर सकेंगे। हां अम्सारे मुस्लिमीन (वे विशुद्ध इस्लामी बस्तियाँ, जिनकी भूमि पर मुसलमानों का स्वामित्व हो और जिसे मुसलमानों ने इस्लामी पहचानों की अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित कर लिया हो। जहां मुसलमानों की इतनी आबादी हो कि वहां जहाँ जुमा और ईदों की नमाज़ होती हो और शरीअत का क़ानून लागू हो।) में इस्लामी सरकार को अधिकार है कि वह उन्हें उसकी आज़ादी दे या न दे। ‘बदाया’ में है:
“जो बस्तियां अम्सारे मुस्लिमीन में नहीं हैं,उन में ज़िम्मियों को शराब और सूअर बेचने और क्रॉस निकालने और घंटियाँ बजाने से नहीं रोका जाएगा, चाहे वहां कितने भी मुसलमान रहते हों। हां, ये गतिविधियां मुसलमानों के बीच घृणित हैं, जहाँ जुमा, ईदें और हुदूद स्थापित की जीती हों.. रही वे बुराईयां, जिसे वे भी बुराई मानते हैं, जैसे कि व्यभिचार और अन्य सभी अश्लीलताएं जो उनके धर्म में भी निषिद्ध हैं, तो इन से उन्हें हर हाल में रोका जाएगा, चाहे मुस्लिम आबादी वाली बस्तियां हों, उन की अपनी आबादी वाली।
लेकिन अम्सारे मुस्लिमीन में भी, उन्हें क्रॉस और मूर्तियों के जुलूस निकालने और खुलेआम घंटी बजाते हुए बाजारों में निकलने की मनाही है। वे अपने प्राचीन उपासनागृहों के भीतर सभी अनुष्ठान कर सकते हैं, इस्लामी प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं है।
(8) अम्सारे मुस्लिमीन के बीच ज़िम्मियों के जो उपासनागृह पहले से मौजूद हों उन्हें छेड़-छाड़ नहीं किया जा सकता है। अगर वे टूट जाएं, तो उन्हें उसी जगह दोबारा बना लेने का अधिकार है, लेकिन नए उपासनागृह बनाने का अधिकार नहीं है। अम्सारे मुस्लिमीन में इन प्रतिबंधों को लागू करने का उद्देश्य यह है कि मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों के बीच संघर्ष के अवसर पैदा न होने पाएं।
(9) ज़िम्मियों को आम तौर पर उन जगहों पर नए उपासनागृह बनाने की अनुमति दी जाती है जो अम्सार मुस्लिम नहीं हैं। इसी तरह वे जगहें जो अब अम्सारे मुस्लिमीन नहीं रहे, और जहां अब जहाँ जुमा और ईदों की नमाज़ नहीं होती हो नए उपासनागृह निर्माण करने और अपने धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन की अनुमति है।
(10) जिज़्या और ख़िराज की वसूली में ज़िम्मियों के साथ ज़ोर ज़बर्दस्ती करना मना है। उनपर कोई ऐसा बोझ न डाला जाए, जो सामर्थ्य से बाहर हो। जिज़्या की मात्रा निर्धारित करने में भी उन पर ज़बर्दस्ती नहीं की जा सकती।
हज़रत उमर ने सीरिया के गवर्नर अबू उबैदा को जो लिखित आदेश दिए, उनमें शामिल था कि: “मुसलमानों को ज़िम्मियों के नुक़सान पहुँचाने से रोकना। मुसलमानों को उन पर अत्याचार न करने देना। उन्हें अवैध तरीक़ों से उनके धन खाने से रोकना।”
सीरिया की अपनी यात्रा के दौरान, हज़रत उमर ने देखा कि उनके एजेंट ज़िम्मियों से जिज़्या लेने के लिए उन्हें दंडित कर रहे थे, इसपर उन्होंने कहा, “इन्हें कष्ट मत पहुँचाओ। अगर तुम इन्हें दंड दोगे, तो अल्लाह तुमको क़ियामत के दिन दंडित करेगा।
(11) जो ज़िम्मी ज़रूरतमंद और ग़रीब हो जाएं, उन्हें न केवल जिज़्या माफ़ कर दिया जाएगा, बल्कि इस्लामी ख़ज़ाने से उन्हें वज़ीफ़ा भी दिया जाएगा।
(12) अगर कोई ज़िम्मी की मृत्यु हो जाए और उसकी ओर जिज़्या बक़ाया हो, तो यह उसकी संपत्ति से नहीं वसूल किया जाएगा और न ही उसके उत्तराधिकारियों पर उसका बोझ डाला जाएगा।
(13) मुस्लिम व्यापारियों की तरह, ज़िम्मी व्यापारियों पर भी उनके व्यापार धन पर कर लगाया जाएगा, जब उनकी संपत्ति 200 दिरहम तक पहुंच जाएगी या वे 20 मिस्क़ाल सोने के मालिक हो जाएं। (किताब अल-खराज: पृष्ठ 70)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन काल में, न्यायविदों ने ज़िम्मी व्यापारियों पर 5% और मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% वाणिज्यिक कर का सुझाव दिया था, लेकिन यह अधिनियम क़ुरआन और हदीस के किसी मूल पर आधारित नहीं था, बल्कि इज्तिहाद और लौकिक हितों के लिए इसकी ज़रूरत थी। उस अवधि के दौरान, मुसलमान ज़्यादातर जिहाद में लगे हुए थे और इस्लामी सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, और सारा व्यापार ज़िम्मियों के हाथों में आ गया था, इसलिए मुस्लिम व्यापारियों के प्रोत्साहन और उनके व्यापार की रक्षा के लिए उन पर कर कम कर दिया गया था।
(14) ज़िम्मियों को सैन्य सेवा से छूट दी गई है और दुश्मन के ख़िलाफ़ देश की रक्षा अकेले मुसलमानों के दायित्व में शामिल है। चूंकि इस सुरक्षा के मुआवज़े के रूप में उनसे जिज़्या वसूल किया जाता है, इसलिए इस्लाम उन्हें सैन्य सेवा का कष्ट देना उचित नहीं समझता है, और न ही उनकी रक्षा करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनसे जिज़्या लेता है। अगर मुसलमान उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें ज़िम्मियों की जिज़्या संपत्ति से लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यर्मूक की लड़ाई के अवसर पर, रोमनों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी सेना एकत्र की और मुसलमानों को सीरिया के सभी विजित क्षेत्रों को छोड़कर एक केंद्र में इकट्ठा होना पड़ा। इस अवसर पर हज़रत अबूउबैदा ने अपने अधिकारियों को लिखा कि अप लोगों ने ज़िम्मियों से जो जिज़्या और लगान लिया है, उसे वापस कर दें और उनसे कहें: “अब हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त धन वापस कर रहे हैं।” इस आदेश के अनुसार, सभी अधिकारियों ने एकत्रित धन वापस कर दिया।
इस्लामी क़ानून के इन कुछ आदेशों की नक़ल केवल यह दिखाने के लिए की गई है कि इस्लाम ने अपने विजित राष्ट्रों के साथ जो न्याय और समानता का व्यवहार किया है, उसकी मिसाल पिछले राष्ट्रों में और ज़्यादातर मामलों में वर्तमान समय के सभ्य राष्ट्रों में भी नहीं मिलती है। यह क़ानून केवल एक काग़ज़ी क़ानून नहीं है बल्कि इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन का प्रभावशाली इतिहास भी है। इसलिए हमने इस क़ानून की हर धारा के साथ हदीस और इतिहास की प्रामाणिक किताबों से कई उदाहरण भी पेश किए हैं ताकि देखने वालों को पता चले कि नबी सल्ल. और उनके साथियों ने क़ानून को कैसे लागू किया। नबी सल्ल. और उनके साथियों के काल के बाद भी इस्लामी न्यायविदों ने हमेशा इस क़ानून को सही तरीक़े से लागू करने की कोशिश की है। और जब विद्रोही शासकों ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है तो विद्वानों और न्यायविदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की है।
इतिहास की प्रसिद्ध घटना है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दमिश्क़ के योहन्ना चर्च को ईसाइयों से बलपूर्वक छीन कर उसे मस्जिद में मिला लिया। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज ख़लीफ़ा बने तो ईसाइयों ने उनसे इस क्रूरता की शिकायत की, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि मस्जिद का जितना हिस्सा चर्च की भूमि पर बनाया गया था उसे ध्वस्त करके वह ईसाइयों के हवाले कर दिया जाए। (फतुह अल-बुलदान: पृष्ठ 122)।
वलीद बिन यज़ीद ने रोमन आक्रमण के डर से साइप्रस के ज़िम्मियों को निर्वासित कर के सीरिया में बसा दिया इस पर इस्लाम के न्यायविद और आम मुसलमान उससे बहुत नाराज हुए। वे इसे एक बड़ा गुनाह मानते थे। फिर जब यज़ीद बिन वलीद उन्हें वापस साइप्रस ले आया तो उसकी प्रशंसा की गई।
ये और इसी तरह के अनगिनत उदाहरण इतिहास में पाए जाते हैं, जो बताते हैं कि इस्लाम के मानने वालों ने हमेशा ज़िम्मियों के अधिकारों का समर्थन किया है और अगर किसी अधिकारी या बादशाह ने कभी उन पर अत्याचार किया है, तो वह इस्लामी क़ानून के विरुद्ध था, इस्लाम उससे दोषमुक्त है।
ज़िम्मियों के पहनावे का सवाल:
हां एक बात इस्लाम में ऐसी पायी जाती है, जिस पर विरोधियों को आपत्ति का मौक़ा मिल जाता है और वह है, ज़िम्मियों के पहनावे का मुद्दा। मगर अफ़सोस की बात है कि आरंभ में उसका जो स्वरूप था, उसे बाद में ग़लत रूप दे दिया गया और इसी से लोगों को यह सोचने का अवसर मिल गया कि इस्लाम ने ज़िम्मियों को अपमानित करने के लिए एक विशेष पोशाक और एक विशेष सामाजिक पद्धति निर्धारित कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर के ज़माने के कुछ संधियों में ऐसी शर्त मौजूद है कि ज़िम्मी लोग एक ख़ास तरह की पोशाक न पहनें और मुसलमानों से समानता न दिखाएं। उदाहरण के लिए, हैरा की संधि में हमें ये शब्द मिलते हैं:
“उन्हें अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने का अधिकार होगा, लेकिन वे सैन्य वर्दी नहीं पहनेंगे और मुसलमानों के साथ समानता नहीं रखेंगे।” (किताब अल-खराज: पृष्ठ (85)
इसी प्रकार, दमिश्क की संधि में, जिसकी शर्तें स्वयं ईसाइयों द्वारा प्रस्तावित की गई थीं, ये शब्द हैं:
“हम मुसलमानों से उनके पहनावे में किसी तरह की समानता नहीं अपनाएंगे, न टोपी में, न पगड़ी में, न जूतियों में, और न मांग निकालने में।” (इब्न कसीर, खंड 4, पृष्ठ 475)
इस तरह के आदेश हमारी न्यायशास्त्र की किताबों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए बदाया में है:
ये अहल अल-दहम दिखाई देने वाली निशानियाँ लेते हैं, वे उन्हें जानते हैं, और वे उन्हें नहीं छोड़ते हैं, और वे अपने पहनावे में मुसलमानों से मिलते जुलते हैं।
“ज़िम्मियों को ऐसे चिन्ह और निशानियां रखनी होंगी जिनसे उनकी पहचान हो सके और उन्हें मुसलमानों से समानता नहीं अपनाने दी जाएगी।”
बेशक ये सभी आदेश हमारे इमामों के हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपमानित करना नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों के लोगों को एक-दूसरे के साथ गड-मड होने से रोकना है। तो जैसे ज़िम्मियों को मुसलमानों के समान होने से रोका गया है, वैसे ही मुसलमानों को भी ज़िम्मियों के समान होने से रोका गया है। पहनावे की समानता में जो बुराइयां छिपी हैं, इस्लाम उन से बेख़बर नहीं है। विशेष रूप से पराधीन राष्ट्रों में प्राय: यह दोष पैदा हो जाता है कि वे अपने राष्ट्रीय पहनावे तथा अपनी राष्ट्रीय सामाजिकता को अपमानजनक समझने लगते हैं तथा प्रभुत्वशाली राष्ट्रों की साज-सज्जा एवं सामाजिक शैली को अपनाने में गर्व का अनुभव करते हैं। दुनिया के पराधीन राष्ट्रों में आज भी यह ग़ुलाम मानसिकता मौजूद है। भारत में ही हम पाते हैं कि स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ अंग्रेज़ी पहनावे पहनते हैं और समझने लगते हैं कि वे विकास के बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं। यद्यपि कभी किसी अंग्रेज़ ने भारतीय पोशाक नहीं पहनी है और अगर उसने विशुद्ध अंग्रेज़ी समाज में कभी पहनी भी है, तो गर्व के लिए नहीं, अपितु उपहास के लिए है। अधीनता के इस मनोविज्ञान को इस्लाम के विद्वान अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने ज़िम्मियों को मुसलमानों की समानता अपनाने से मना करके अपमानित नहीं किया, बल्कि उनके राष्ट्रीय पहचान और सम्मान को बनाए रखा। संभव है कि इस प्रकार के क़ानून कुछ लोगों की दृष्टि में तिरस्कारपूर्ण हों। लेकिन हमारे लिए इसमें कोई तिरस्कार नहीं है, बल्कि हमें बहुत ख़ुशी होती अगर पराधीन भारत में ब्रिटिश शासकों ने भी हमें अंग्रेज़ी पहनावे और सामाजिकता अपनाने से मना किया होता।
(5) कुछ अपवाद
युद्ध और उससे संबंधित इस्लाम द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों, सीमाओं और प्रतिबंधों की उपरोक्त पृष्ठों में विस्तार से व्याख्या कर दी गई है। लेकिन पैग़म्बरे इस्लाम और इस्लाम के ख़लीफ़ाओं के ज़माने में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो इन क़ानूनों से अलग नज़र आती हैं और जो व्यक्ति इनसे परिचित नहीं है उन्हें शक हो सकता है कि इस्लाम के मूल क़ानून वे नहीं हैं जो वर्णित किये गये हैं, या उसके आदेशों में विरोधाभास हैं, या अल्लाह के रसूल और सहाबा के कार्य इस्लामी क़ानूनों के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इस अध्याय को समाप्त करने से पहले, इन अपवादों की व्याख्या करना आवश्यक है।
बनु नज़ीर का निष्कासन
इस श्रृंखला की पहली घटना बनू नज़ीर का निष्कासन है। यह यहूदियों का एक क़बीला था जो सदियों से यसरिब (मदीना) में रह रहा था। प्रवास के बाद, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने उनके साथ एक समझौता किया और बद्र की लड़ाई के बाद, उन्होंने उन्हें मदीना से निकाल दिया। विरोधियों ने इस घटना की व्याख्या इस अर्थ में की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नज़ीर के साथ धोखा किया, अर्थात् जब कमज़ोर थे, तो उनके साथ संधि की, और जब शक्तिशाली हो गए, तो समझौता तोड़ कर उन्हें देश-निकाला दे दिया।
यह उस घटना का एक साधारण रूप मान लेने का ही परिणाम है, अन्यथा अगर इसके सभी विवरणों पर ग़ौर किया जाए तो घटना बिल्कुल विपरीत नज़र आएगी। संधि-उल्लंघन के दोषी अल्लाह के रसूल (सल्ल.) नहीं, ख़ुद बनू नज़ीर निकलेंगे और उनके विरुद्ध युद्ध की कार्रवाई अन्याय नहीं, बल्कि न्याय सिद्ध होगी।
जब अल्लाह के रसूल (सल्ल.) मक्का से निकलकर मदीना आए तो उन्होंने यहूदियों के अन्य क़बीलों की तरह बनू नज़ीर से भी एक समझौता किया था, जिसकी मुख्य शर्त यह थी कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे और एक-दूसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे।
इस समझौते के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) और आम मुसलमान उनकी ओर से निश्चिंत हो गए और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध शुरू कर दिया था। लेकिन बनू नज़ीर ने समझौते की शर्तों के ख़िलाफ़ अवज्ञाकारी क़ुरैश के साथ षड्यंत्र करना जारी रखा और गुप्त रूप से उन्हें मुसलमानों के बारे में जानकारी पहुंचाने लगे।
“फिर वे इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कई बार पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) को जान से मारने की कोशिश भी की। एक बार, उन्होंने नबी को यह कहला भेजा कि आप अपने साथ तीन आदमी ले कर आएं और हम भी अपने तीन विद्वानों को भेजेंगे। बीच के किसी स्थान पर उनसे बहस होगी और अगर आप अपने दीन की सच्चाई साबित कर देंगे तो हम आप पर ईमान ले आएगे। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने यह न्यौता कुबूल कर लिया। लेकिन अभी वे निश्चित स्थान के लिए निकले ही थे जब बनू नज़ीर की एक औरत ने ख़ुद अपने भाई को जो कि एक मुसलमान था, बताया कि यहूदी ख़ंजर लेकर आ रहे हैं और तुम्हारे पैग़म्बर (सल्ल.) को मारने का इरादा रखते हैं। यह सुनकर नबी ने जाने का इरादा छोड़ दिया।
एक अन्य अवसर पर, अल्लाह के रसूल (सल्ल.) बनू आमिर के दो व्यक्तियों के ख़ून के हर्जाने के मामले को निपटाने के लिए बनू नज़ीर के पास गए। उन लोगों ने बाहरी तौर पर मित्रवत व्यवहार किया और नबी से कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपस में जाकर सलाह की कि यह व्यक्ति फिर से ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं इसका काम तमाम कर दिया जाए। अत: नबी जहां बैठे थे उस घर की छत पर एक आदमी एक भारी पत्थर लेकर बैठ गया कि कि वहां से उसे नबी पर फेंक दे। लेकिन ठीक समय पर उनको उसकी सूचना मिल गई और वे उठकर वहां से चले आए।
लगातार विश्वासधात और साज़िशों के चलते ये डर था कि कहीं आस्तीन के ये सांप किसी बाहरी हमले के दौरान मदीना की सुरक्षा को ख़तरे में न डाल दें। यह आशंका भी थी कि कहीं ये लोग गुपचुप तरीक़े से अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की हत्या न कर दें। ऐसे में विश्वासधाती दुश्मनों की और अधिक अनदेखी नहीं की जा सकती थी, लेकिन नबी करीम ने फिर भी उन्हें रियायतें दीं और उन पर तुरंत हमला करने के बजाय, उन्होंने मुहम्मद बिन मुस्लिम के माध्यम से उन्हें यह अल्टीमेटम दिया:
“तुमने मेरे साथ ग़द्दारी की है, इसलिए या तो तुम ख़ुद दस दिनों के भीतर मदीना ख़ाली कर दो, अन्यथा मुझे तुम से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।”
उधर मुनाफ़िक़ों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने उन्हें यह कहला भेजा कि तुम मुहम्मद की बात कभी न मानना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के अल्टीमेटम का यह जवाब दिया कि:
“हम अपनी भूमि नहीं छोड़ेंगे, तुम जो चाहे कर लो।”
इसके बाद कौन कह सकता है कि अल्लाह के रसूल उनके विरुद्ध युद्ध करने में न्यायसंगत नहीं थे? अनुबंध के स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में जो अधिकतम उदारता हो सकती है, वह उन्होंने की। अंत में वे युद्ध के लिए विवश हो गए और उन्होंने उन्हें घेरे में ले लिया, इससे पहले कि रक्तपात होता बनू नज़ीर घबरा गए और उन्होंने ख़ुद सुझाव दिया कि आप हमारा ख़ून माफ़ कर दें, हम मदीना छोड़ देंगे और अजरात (सीरिया) चले जाएंगे। हमारे ऊंट जो कुछ भी सामान ले जा सकते हैं, हम ले लेंगे और बाक़ी सब कुछ यहीं छोड़ देंगे। इस शर्त को पैग़म्बरे इस्लाम ने स्वीकार कर लिया और बनू नज़ीर इस्लामी क्षेत्र को छोड़ कर बिना कोई नुक़सान उठाए सीरिया की ओर चले गए।
स्पष्ट है कि युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद ऐसी स्थिति में जब उन्हें आसानी से पराजित कर बदला लिया जा सकता था, उनकी शर्तों को स्वीकार करना और उन्हें शांति और सुरक्षा में रहने देना, और उन्हें अपनी संपत्ति के साथ जाने देना, शांतिप्रियता नहीं तो और क्या है। ऐसा काम वही कर सकता था जिसका मक़सद ख़ूनख़राबा और लूटपाट नहीं, बल्कि केवल बुराई को दूर करना हो। अल्लाह ने अपने पैग़म्बर को समस्त जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा था, यह उनकी शान के ख़िलाफ़ था कि वे एक हारे हुए दुश्मन की दया की भीख को ठुकरा देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि ये षडयंत्रकारी चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने माफी मांगी तो नबी ने तुरंत माफ़ कर दिया।
बनू क़ुरैज़ा की घटना
बनू क़ुरैज़ा के नरसंहार की धटना को और अधिक आपत्तियों का विषय बनाया गया है। ये लोग भी धार्मिक रूप से यहूदी थे और बनू नज़ीर की तरह मदीना में बस गए थे। जब पैग़म्बर (सल्ल.) मदीना आए, तो उन्होंने उनके साथ वही समझौता किया जो अन्य यहूदी क़बीलों के साथ किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। फिर जब बनू नज़ीर के साथ युद्ध हुआ तो नबी ने फिर से बनू क़ुरैज़ा को एक संधि के लिए आमंत्रित किया और प्राचीन संधि का नवीनीकरण कर लिया। लेकिन जब अहज़ाब युद्ध में उन्होंने खुले तौर पर दुश्मनों का साथ दिया, तो उधर से निपटने के बाद उन्होंने उन पर हमला कर दिया। उनके वयस्क पुरुषों को मार डाला, उनके बच्चों और महिलाओं को ग़ुलाम बना लिया और उनकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया। इस घटना को लेकर विरोधियों ने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) पर विश्वासघात और क्रूरता का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन जब बारीकी से देखा जाए तो इसकी वास्तविकता भी विरोधियों के दावों से बिल्कुल अलग है।
ऊपर कहा जा चुका है कि बनू क़ुरैज़ा के साथ दो समझौते किए गए थे। एक सामान्य समझौता, जो अन्य यहूदी जनजातियों की उपस्थिति में किया गया था, और बनी नज़ीर से युद्ध के बाद उनके साथ एक विशेष समझौता किया गया था। इन दोनों समझौतों के बाद, बनू क़ुरैज़ा का यह दायित्व था कि व अल्लाह के रसूल, के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में हिस्सा न लेते। लेकिन अहज़ाब (समुदायों) के युद्ध में जब बनू नज़ीर के उकसाने पर अरब के प्रमुख क़बीलों ने इस्लाम को नष्ट करने के लिए मदीना पर हमला किया, तो बनू क़ुरैज़ा ने भी समझौते को तोड़ दिया और युद्ध में शामिल हो गए। अल्लाह के रसूल (सल्ल.) को उनके समझौता भंग करने के बारे में पता चला, तो उन्होंने साद बिन मुआद और साद बिन उबादह को उनके पास भेजा और उन्हें अपना वादा निभाने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने साफ़ कहा कि हमारा तुमसे कोई समझौता नहीं है।
उनके द्वारा ऐसे समय पर समझौता तोड़ कर युद्ध में शामिल हो जाने से मदीना दोनों ओर से घिर गया। एक ओर क़ुरैश वग़ैरह की फौजें थीं और दूसरी ओर बनू क़ुरैज़ा। सबसे बड़ा ख़तरा यह था कि जिस क़िले में मुसलमानों ने अपनी महिलाओं को सुरक्षा के लिए भेजा था, वह बनू क़ुरैज़ा के सीधे निशाने पर था और वे उसे घेरने की धमकी दे रहे थे। इस स्थिति ने मुसलमानों को अत्यधिक आतंक और चिंता से ग्रस्त कर दिया। यहां तक कि पवित्र पैग़म्बर (सल्ल.) मजबूर होकर मदीना के उत्पादन का तीसरा हिस्सा देकर आक्रमणकारियों के साथ समझौता करने का विचार करने लगे। इस समस्या की स्थिति पवित्र क़ुरआन में इस प्रकार वर्णित है:
إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠○ (الاحزاب: ۱۰)
“जब कि वे तुम पर नगर के ऊपर से और निचले भाग की ओर से चढ़ आए, और जब कि तुम्हारी आंखों में अन्धेरा छा गया, और जब दिल मुँह को आने लगे और तुम अल्लाह के बारे में तरह-तरह की बुरी धारणाएँ बनाने लगे।” (अहज़ाब:10)
हज़रत हुज़ैफ़ा इस आयत की व्याख्या करते हैं:
“उस रात हमारी चिंता और परेशानी हद से बढ़ी हुई थी। एक ओर अबू सुफ़ियान और उसके साथी एक बड़ी सेना के साथ ऊपर से आए, और दूसरी ओर, बनू क़ुरैज़ा नीचे से आए, और उनके हमले से हमारे बाल-बच्चों की सुरक्षा को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया।”
इस घोर और ख़तरनाक विश्वासघात के बाद इन लोगों को कोई छूट देना आत्मघाती था। इसलिए, जब अहज़ाब के बादल छट गए और बाहरी हमले का डर नहीं रहा, तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने तुरंत बनू क़ुरैज़ा को घेर लिया। 15 दिन या 35 दिन इस्लामी सेनाएं उनके क़िले के आसपास डटी रहीं। जब उन्होंने देखा कि मौत का यह संदेश टल नहीं सकता है, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की सेवा में यह संदेश भेजा कि साद बिन मुआज़ हमारे पक्ष में जो फ़ैसला करेंगे, हम उसे स्वीकार करते हैं। कुछ किताबों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपने भाग्य का फ़ैसला अल्लाह के रसूल (सल्ल.) पर छोड़ दिया और उन्होंने साद बिन मुआज़ को इस विचार से ‘हकम’ (मध्यस्थ) बना दिया कि वे बनू क़ुरैज़ा के सहयोगी थे, कोई भी उन पर शक नहीं कर सकता था कि वे उनके पक्ष में कोई अनुचित निर्णय लेंगे। बहरहाल, साद ने फ़ैसला कर दिया कि बनू क़ुरैज़ा के वयस्क पुरुषों को मार डाला जाए, महिलाओं और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए और उनकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाए। अत: इसी निर्णय को लागू किया गया।
अब कोई यह नहीं कह सकता कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उन पर हमला करके अपना वादा तोड़ा। लेकिन दूसरा आरोप यह रह जाता है कि उनके ख़िलाफ़ बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन इसे सख़्त और कठोर हृदयता कहने से पहले, कुछ मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए:
(1) बनू क़ुरैज़ा और उनके सहजाति, बनू नज़ीर के विश्वासघातों को देखते हुए, उनके साथ फिर से एक नया समझौता करना और यह उम्मीद करना व्यर्थ था कि वे इसे किसी आड़े समय में नहीं तोड़ देंगे।
(2) उनके क़िले मदीना से लगे हुए थे और इस तरह के घोर विश्वासघात के बाद, उनके इतने क़रीब होने से यह ख़तरा हमेशा बना रहता कि वे कब मुसलमानों के घरों पर हमला कर दें।
(3) उन्हें देश निकाला भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उससे पहले उनके भाई बनू नज़ीर के निर्वासन का परिणाम यह हुआ कि वे मुसलमानों से दूर बैठकर युद्ध की तैयारियां करते रहे और सेना इकट्ठी करके मदीना पर चढ़ आए।
(4) इन बातों के बावजूद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने ख़ुद उनके लिए कोई सज़ा प्रस्तावित नहीं की, बल्कि अपनी इच्छा और सहमति से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया जो ख़ुद उनका पुश्तैनी सहयोगी था।
(5) मध्यस्थता और पंचायत के संबंध में, यह पूरे विश्व का एक स्थापित क़ानून है कि जब किसी व्यक्ति को दोनों पक्षों की सहमति से, मध्यस्थ या पंच बनाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए निर्णय को मानना पक्षों पर अनिवार्य होता है।
(6) साद बिन मुआज़ ने जो फ़ैसला किया वह तौरात के नियमों के अनुसार था। इसलिए किसी यहूदी ने उनके ख़िलाफ़ एक शब्द नहीं कहा।
(7) उनमें से केवल वे पुरुष मारे गए जो हथियार उठाने में सक्षम थे, क्योंकि उनसे ही ग़द्दारी की आशंका थी। बाक़ी रहीं औरतें और बच्चे, उनके पालन-पोषण का इसके सिवा और क्या साधन हो सकता था कि मुसलमान ख़ुद उनके अभिभावक बन जाएं।
इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बनू क़ुरैज़ा के साथ जो कुछ किया गया वह सटीक न्याय था, उनके साथ कोई अन्य उपचार नहीं किया जा सकता था।
ख़ैबर के यहूदियों का निष्कासन
पैग़म्बर (सल्ल.) के बाद ख़िलाफ़त काल के दौरान ख़ैबर के यहूदियों के निष्कासन को विशेष रूप से निंदा का लक्ष्य बनाया गया है। विरोधियों का कहना है कि जब अल्लाह के रसूल ने ख़ैबर के लोगों के साथ आधे उत्पादन पर समझौता कर लिया था और वे स्थायी रूप से इस्लाम की प्रजा बन गए थे, तो हज़रत उमर को उन्हें निर्वासित करने का क्या अधिकार था? क्या इस तरह उन्होंने वादा नहीं तोड़ा और ज़िम्मियों के अधिकारों का हनन नहीं किया? यह आपत्ति ज़ाहिर तौर पर बहुत वजनदार है, लेकिन इतिहास ने उन सभी तथ्यों को संरक्षित रखा हुआ है जिससे इस आपत्ति का खोखलापन स्पष्ट हो जाता है।
जब ख़ैबर पर विजय प्राप्त की गई, तो यहूदियों की शुरू में अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ इस शर्त पर संधि हुई थी कि वे उनकी जान बख़्श देंगे और वे उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन शांति के बाद, जब भूमि की नियमित व्यवस्था का अवसर आया, तो ख़ैबर के लोगों ने पैग़म्बर (सल्ल.) से अनुरोध किया कि आप हमें यहीं रहने दें और हम से मामला कर लें, क्योंकि हम खेती और मरूद्यान के काम से भली भांति परिचित हैं।”
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनके साथ एक अस्थायी समझौता कर लिया। लेकिन समझौते की शर्तों को लिखते समय, यह स्पष्ट व्याख्या कर दी कि जब तक अल्लाह तुम्हें बनाए रखेगा, मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। इसका मतलब यह था कि तुमको स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा, बल्कि जब तक हमारे राष्ट्रीय हित में हमें अल्लाह के आदेशों के अनुसार तुम्हें रखने की अनुमति होगी, तब तक रहने दिया जाएगा। और जब तुम्हारा व्यवहार अनुचित होगा तो हम इस शांति समझौते की शर्तों के अनुसार, तुमको निर्वासित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इससे यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उनके साथ ऐसा कोई समझौता नहीं था जिसके आधार पर उनके निष्कासन को वचनभंग कहा जा सके। इसके विपरीत वास्तविक समझौता उनके निष्कासन की ही मांग करता था। अब रहा यह प्रश्न कि आधे लगान के आधार पर उनके साथ जो अस्थायी समझौता किया गया था, उसे क्यों निरस्त किया गया? इसके शोध के लिए निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए:
सुलह के कुछ ही दिन गुज़रे थे कि उनमें से एक महिला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की और उन्हें ज़हर खिला दिया। बाद में जब जांच की गई तो अपराधी ने ख़ुद अपना जुर्म क़ुबूल कर लिया और इस कृत्य में अन्य यहूदियों की साज़िश भी साबित हुई।
अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ही के समय में, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन सहल बिन ज़ैयद अल-अंसारी को मार डाला और उन्हें एक नहर के किनारे फेंक दिया।
हज़रत उमर के समय में उन्होंने खुले तौर पर बगावत की और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को नींद में उठाकर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उनके हाथ टूट गए।
प्रारंभिक घटनाएं कुछ लोगों के साथ विशिष्ट थीं, इसलिए आम जनता को उनके अपराध के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था। लेकिन यह आख़िरी अपराध सरेआम किया गया था और पूरे राज्य का दुश्मनी का तेवर दिखाई दे रहा था, इसलिए हज़रत उमर ने इस मामले को सहाबियों की सभा में पेश किया और इस पर अपनी राय देते हुए कहा:
“अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ख़ैबर के यहूदियों के साथ उनकी संपत्ति पर समझौता किया था और कहा था, “जब तक अल्लाह तुम्हें बनाए रखता है, हम तुम्हें बनाए रखेंगे।” अब अब्दुल्लाह इब्ने उमर वहां अपनी जागीर पर गए थे, उन पर रात में हमला किया गया और उनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए। इस देश में उनके सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वे ही हमारे दुश्मन रह गए हैं। इसलिए मेरी राय में उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए।”
सभी सहाबियों ने हज़रत उमर के प्रस्ताव से सहमति जताई और यहूदियों को देश से निकालने का फ़ैसला हो गया। इसके बावजूद उन अपराधियों को इस तरह निर्वासित नहीं किया गया कि उनकी संपत्ति ज़ब्त कर ली जाए और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जो कुछ वे छोड़ गए, उसका पूरा मुआवज़ा उन्हें बैतुलमाल से दिया गया। यात्रा में आसानी के लिए ऊंट और कुजावे दिए गए, यहां तक कि कुजावे बांधने के लिए रस्सियां भी दी गईं। (बुख़ारी: किताब अल-शुरूत)
नजरान के लोगों का निष्कासन
सच्चे ख़लीफ़ाओं के काल की एक और महत्वपूर्ण घटना, जो ख़ैबर मामले से भी अधिक आलोचना का विषय रही है, नजरान के ईसाइयों का निष्कासन है। ख़ैबर के यहूदियों पर विजय प्राप्त हुई थी और उनके साथ निष्कासन की शर्त पर ही समझौता हुआ था, इसलिए विरोधियों को इसमें आपत्ति के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल सकी। लेकिन नजरान के लोगों ने बिना किसी युद्ध के स्वतः ही आज्ञाकारिता स्वीकार कर ली थी और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के साथ जिज़्या देकर एक औपचारिक समझौता किया था। इसलिए उनके निष्कासन को इस्लाम के विरोधी समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानते हैं। उनका तर्क है कि अनुबंध में बिना शर्त शांति दी गई थी और हज़रत उमर ने अवैध रूप से उस शांति को रद्द कर दिया। लेकिन घटनाक्रम की पड़ताल इस दावे को ग़लत साबित करती है।
नजरान के साथ अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की जो संधि हुई थी, उसमें, ईसाइयों को इस शर्त के साथ शांति प्रदान की गई थी कि जब तक वे इस्लामी सरकार के प्रति वफ़ादार रहेंगे, और अपने दायित्व का भुगतान करते रहेंगे, तब तक उन्हें अल्लाह की पनाह और अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की सुरक्षा प्राप्त रहेगी।
फिर, हज़रत अबू बक्र ने ख़िलाफ़त का पद संभालने के बाद, उनको जो समझौता लिख कर दिया उसमें भी स्पष्टीकरण के साथ लिखा था कि:
“यह उनका दायित्व है कि वे शुभचिंतक बने रहें और जो भी उनका दायित्व है, उन्हें पूरा करते रहें।”
इस समझौते के अनुसार जिस तरह इस्लामी सरकार ने उनकी रक्षा करने और उनकी प्राचीन स्थिति को बनाए रखने का वचन दिया था, उसी तरह उन्होंने नजरान के लोगों से भी प्रतिज्ञा ली थी कि वे इस्लामी सरकार के प्रति वफ़ादार रहेंगे। यह वही प्रतिज्ञा है, जो दुनिया की हर सरकार अपने नागरिकों से लेती है। लेकिन नजरान के लोगों ने इस वादे को कहां तक पूरा किया? और वफ़ादारी का हक़ कहाँ से अदा किया, इसका जवाब इतिहास से यह मिलता है कि उन्होंने घोड़े और शस्त्र जमा कर विद्रोह की तैयारी की और इस्लामी हुकूमत के केंद्र को ख़तरे में डाल दिया।
अरब के नक्शे पर नज़र डालें तो साफ़ हो जाएगा कि नजरान के लोगों की ये तैयारियां किस तरह के ख़तरों का संकेत थीं। एक ओर, उनके उत्तर में इस्लामी शासन का केंद्र हिजाज़ था, और दूसरी ओर, उनके सामने, लाल सागर के दूसरे किनारे पर, अबीसीनिया का ईसाई राज्य था। अगर वे अपनी तैयारी पूरी कर लेते और हिजाज़ पर हमला कर देते और अबीसीनिया के अपने सह-धर्मियों को अबरहा की अधूरी योजना को पूरा करने में अपनी मदद करने के लिए बुला लेते, तो हर कोई अनुमान लगा सकता है कि मुसलमानों को कैसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ता।
इतिहासकारों ने लिखा है कि शांति और व्यवस्था की बरकत से उनकी जनसंख्या बढ़कर चालीस हज़ार हो गई थी और धन की अधिकता ने उनके बीच गृहयुद्धों का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। उनके अलग-अलग गुट हज़रत उमर से एक दूसरे की शिकायत करते थे और हर गिरोह के लोग दूसरे गिरोह को निकालने की सलाह देते थे। पहले तो हज़रत उमर इसकी अनदेखी करते रहे, लेकिन जब उनकी बढ़ती शक्ति से ख़ुद इस्लामी हुकूमत के केंद्र को ख़तरा होने लगा तो उन्होंने इस मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें देश-निकाला देने का आदेश दे दिया।
हालाँकि, एक राष्ट्र जिसके ख़िलाफ़ विद्रोह की तैयारी के प्रमाण तक मौजूद थे, उसे इस्लामी शासन की सीमाओं से बाहर नहीं किया गया था, बल्कि केवल अरब से बाहर किया गया था। वे अल्लाह की शरण और मुहम्मद, पैग़म्बर (सल्ल.) की ज़िम्मेदारी से वंचित नहीं किये गये, बल्कि उसी शरण और ज़िम्मेदारी में एक अनुचित स्थान से दूसरे उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित कर दिये गये थे। नजरान से उनके निष्कासन का उद्देश्य केवल उन्हें हिजाज़ और एबिसिनिया के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य स्थिति पर क़ब्ज़ा करने से रोकना था। कोई अन्य सज़ा का इरादा नहीं था। इसलिए, हज़रत उमर ने उन्हें यमन के नजरान से स्थानांतरित करके इराक़ के नजरान भेज दिया। उन्हें उनकी ज़मीनों के बदले में ज़मीनें दीं, दो साल का जिज़्या माफ़ किया, उनके लिए यमन से इराक़ की यात्रा की सारी सुविधा दी और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे उन्हें कोई असुविधा न होने दें।
आपत्ति करनेमालों ने इन सभी बातों को भूला कर केवल इतना याद रखा कि नजरान के लोगों के साथ एक समझौता था, हज़रत उमर ने इसे तोड़ दिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखकर कोई हमें बताए कि आज के समय में भी अगर कोई राष्ट्र वह रवैया अपनाता है जो नजरान ने अपनाया था और उसकी राजनीतिक और सैन्य स्थिति भी वही हो जो नजरान की थी, तो एक सभ्य सरकार जो अपने राज्य की शांति को बनाए रखना चाहती है, उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी?
(6) युद्ध के आधुनिक क़ानूनों की स्थापना
इस अध्याय में जो प्रस्तुत किया गया है, उसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस्लामी शरीयत ने युद्ध के व्यावहारिक पहलुओं में से किसी भी पहलू को एक मज़बूत क़ानून द्वारा विनियमित किए बिना नहीं छोड़ा है। उसने युद्ध के वे सभी बर्बर तरीक़ों पर रोक लगा दी, जो दुनिया में प्रचलित थे। युद्ध और उससे जुड़ी चीज़ों के लिए नए सभ्य क़ानून निर्धारित किये। कुछ पुराने तरीक़ों को समय की भावना के अनुसार संशोधित रूप में अगर बनाए भी रखा, तो उनमें क्रमिक सुधार का ऐसा लचीलापन पैदा कर दिया कि समय की प्रगति और परिस्थितियों के परिवर्तन और मानवीय विचारों के विकास के साथ-साथ उनमें स्वत: ही सुधार होता चला जाए। इसी प्रकार कुछ नए नियम भी बनाए गए, जिनमें उनमें विकास की ऐसी क्षमता थी कि प्रत्येक युग की ज़रूरत के अनुसार उनसे उपनियम निकाले जा सकते हैं। इसके साथ ही पैग़म्बर (सल्ल.) और उनके साथियों ने अभ्यास का एक उदाहरण छोड़ा है जो शरीयत की भावना को पूरी तरह से दर्शाता है और इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम हर नई स्थिति में पता लगा सकते हैं कि इस विषय में इस्लाम का पक्ष क्या है।
प्रारंभिक शताब्दियों में, न्यायविदों ने उसी सामग्री से युद्ध के क़ानूनों का एक पूरा कोड संकलित किया, जो सदियों से इस्लामी साम्राज्यों में प्रचलित रहा। लेकिन उस समय के युद्ध के नियम आज की परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उस युग में जिन विवरणों पर काम किया गया था, उनमें से कई आज बेकार हैं। आधुनिक सैन्य पद्धतियों और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण जो नई परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, उनके बारे में आदेश और निर्देश प्राचीन न्यायशास्त्रियों की किताबों में उपलब्ध नहीं हैं। इस लिए ज़रूरत है कि हम मूल स्रोत अर्थात क़ुरआन और हदीस से सिद्धांतों और संकेतों के लेकर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क़ानून तैयार कर लें।
उदाहरण के लिए, क़ुरआन और हदीस में, हमें युद्ध-बंदियों, घायलों,बीमारों, और तटस्थों के अधिकारों और दायित्वों और ऐसे ही दूसरे मुद्दों के बारे में केवल सिद्धांत मिलते हैं, इन मुद्दों के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता। इन ग़ैर-विस्तृत सिद्धांतों का अर्थ यह है कि शरीयत हर युग के मुसलमानों को यह अधिकार देती है कि वे अपने समय की ज़रूरतों के अनुसार अपने नियम बना सकते हैं। इसलिए, हमें इन विषयों के लिए हिजरी की 5वीं और 6वीं शताब्दी में लिखी गई न्यायशास्त्र की किताबों पर निर्भर करने और उनमें पाए जाने वाले विवरणों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि हमारा काम अपने समय की परिस्थितियों को देखना और शरीयत के उसूलों से ऐसे क़ानून बनाना है जो मौजूदा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों।
इसे ध्यान में रखते हुए, इस अध्याय में, मैंने शरिया के मूल स्रोतों, यानी क़ुरआन और हदीस से सिद्धांतों और संकेतों की नक़ल कर दी है, जो एक पूर्ण क़ानून के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। इसके साथ ही पिछले विद्वानों की व्याख्याएँ जहाँ-जहाँ आधुनिक युग की भावना के अनुरूप पायी गयी हैं, उनकी नक़ल भी कर दी है। उन अपवादों का भी उल्लेख कर दिया है, जिनकी बाहरी शक्ल-सूरत देखकर, लोगों को यह शंका होती है कि इस्लामी क़ानून के भीतर विरोधाभास है।
छठा अध्याय
युद्ध अन्य धर्मों में
जब किसी चीज़ के दोषों और गुणों की जांच की जाती है, तो पहले यह देखा जाता है कि वह अपने-आप में कैसी है। फिर यह देखा जाता है कि अन्य चीज़ों के बीच उसका स्वरूप क्या है। जब वह उन दोनों आधारों पर बेहतर साबित हो जाए तभी उसे स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। जहां तक शोध की इस पद्धति के संदर्भ में पहले चरण का संबंध है, हमने इसे पूरा कर लिया है। अब हमारे सामने दूसरा चरण है। इसमें हम पहले इस्लाम की तुलना अन्य धर्मों से करेंगे, और फिर उसकी तुलना आधुनिक समय के क़ानूनों से करके यह अध्ययन करेंगे कि युद्ध के मामले में उनका तरीक़ा इस्लाम के तरीक़े से क्या संबंध रखता है। अगर वे युद्ध को जायज ठहराते हैं तो उनका उद्देश्य और तरीक़ा इस्लाम से अच्छा है या बुरा। अगर वे युद्ध को जायज़ नहीं मानते तो इस विषय में उनकी शिक्षा क्या है। क्या वह मानव स्वभाव के अनुकूल है या इस्लाम की शिक्षा मानव स्वभाव के अनुकूल है।
धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के सिद्धांत
धर्मों की तुलना करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। आदमी जिस आस्था और मत पर विश्वास रखता है, उसके विरुद्ध आस्था और मतों के साथ बहुत कम न्याय कर सकता है। यह कमज़ोरी मानव स्वभाव में बहुत आम है। विशेष रूप से धार्मिक समूहों में इसने पूर्वाग्रह और संकीर्णता का निकृष्टतम रूप धारण कर लिया है। जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं, तो वे हमेशा उनके कमज़ोर पक्ष की तलाश करते हैं और उज्ज्वल पक्ष को देखने की कोशिश नहीं करते हैं या अगर वे उसे देखते भी हैं, तो वे जानबूझकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक आलोचना से, उनका उद्देश्य वास्तविक सत्य की तलाश करना नहीं होता, बल्कि केवल उस राय को सही ठहराना होता है, जिसे वे शोध से पहले अपना चुके हैं। इस विधि से धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की सभी उपयोगिताएं समाप्त हो जाती हैं और स्वयं उस धर्म को भी कोई लाभ नहीं होता, जिसके समर्थन में यह भ्रामक पद्धति अपनाई जाती है ।अगर तुलना का उद्देश्य वास्तव में सत्य का शोध ही है, तो निश्चित रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति का यह तरीक़ा उचित नहीं है कि व्यक्ति पहले से ही अन्य धर्मों के बारे में शत्रुतापूर्ण राय बना ले और उनका अध्ययन केवल इस इरादे से करे कि उनके गुणों पर पर्दा डालना है और उनके दोषों को खोजकर उनके आधार पर अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करनी है। इस प्रकार की बेईमानी और धोखेबाज़ी से किसी धर्म की श्रेष्ठता की पुष्टि वास्तव में उसकी श्रेष्ठता नहीं होगी। ऐसी सफलता किसी भी धर्म के लिए गौरव का कारण भी नहीं हो सकती है और न ही ऐसे धर्म का सत्य और धार्मिकता की दृष्टि में कोई मूल्य होगा। इस प्रकार का धोखा खाकर अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की सच्चाई पर विश्वास कर लेता है, तो यह विश्वास भरोसा योग्य नहीं होगा, क्योंकि उसकी नींव ही ग़लत होगी।
इन त्रुटियों से बचकर धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा को किसी उचित निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि पहले तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ नियम निर्धारित कर लिए जाएं और उनका सख़्ती से पालन किया जाए। हमारी राय में वे सिद्धांत ये होने चाहिए:
(1) एक धर्म की शिक्षाओं को सही साबित करने के लिए, दूसरे धर्मों की शिक्षाओं को पूरी तरह से ग़लत साबित करना आवश्यक नहीं है। एक धर्म में सत्य के अस्तित्व का अर्थ यह कदापि नहीं है कि दूसरे धर्म में उसका अस्तित्व नहीं है। सत्य एक सार्वभौमिक वास्तविकता है जिसके सदस्य, चाहे वे कहीं भी हों, उसी एक संपूर्णता के सदस्य बने रहते हैं। स्थिति और स्थान बदलने से उनकी वास्तविकता नहीं बदलती। जो सत्य हमारे धर्म में पाया जाता है, उसी का दूसरे धर्म में पाया जाना, दोनों धर्मों में से किसी के भी दोष का प्रमाण नहीं है, कि उसपर पर्दा डालने का पर्यास किया जाए, बल्कि वास्तव में यह इसका प्रमाण है कि दोनों एक ही स्रोत से आए हैं। इसलिए सत्य जितना भी कहीं विद्यमान है, उसकी अपेक्षा है कि उसका सम्मान किया जाए, खींच-तान कर उसे मूल्यहीन सिद्ध करने में ज़ोर न लगाया जाए।
(2) जो व्यक्ति यह दावा करता है कि सत्य उसके धर्म के सिवा कहीं और मौजूद नहीं है, वह केवल अन्य धर्मों ही के साथ नहीं, स्वयं सत्य के साथ भी अन्याय करता है। सच तो यह है कि सत्य का प्रकाश न्युनाधिक हर जगह मौजूद है। हालाँकि, शोधकर्ता जब एक धर्म को दूसरे धर्मों पर वरीयता देते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी नज़र में वह धर्म वास्तविकता की अभिव्यक्ति होता है। इसलिए धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने वालों को भी पहले से यह निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि उसके पसंदीदा धर्म को छोड़कर सभी धर्म सत्य के प्रकाश से ख़ाली हैं, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि उसके सामने सत्य और असत्य दोनों मिले-जुले आएंगे और उनका काम यह होगा कि अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में देखे और एक को दूसरे के साथ गडमड न होने दे।
(3) धार्मिक शोध में इस का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी धर्म के द्वेशपूर्ण विरोधियों और धर्म के भावुक अनुयायियों दोनों के लेखन का अध्ययन करने से बचा जाए। प्रारंभिक शोध में ऐसे लोगों के लेखन का अध्ययन करके एक पाठक कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इस के तहत धर्म के असली चेहरे को देखने से पहले ही उसकी आंखों पर एक विशेष रंग की ऐनक चढ़ जाती है, जिससे वह उस धर्म को उसके असली रंग में नहीं देख सकता। अगर इस जाँच को किसी सही निष्कर्ष पर पहुँचाना है, तो यह आवश्यक है कि किसी धर्म को उस रूप में न देखा जाए, कि दूसरे उसे किस रूप में देखते हैं, बल्कि उस रूप में देखा जाए, जिसमें वह स्वयं को प्रकट करता है। इसके लिए यथासम्भव प्रत्येक धर्म के मौलिक स्त्रोतों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें पढ़कर अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि वह धर्म कहाँ तक सही है और कहाँ तक ग़लत है। फिर जब मनुष्य अपना एक मत स्थापित कर ले तो दूसरों के मतों का अध्ययन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तब वह सही और ग़लत में आसानी से भेद कर सकेगा।
आगे के पृष्ठों में युद्ध के विषय में विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा में इन्हीं तीन सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है और ऐसा करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि अपने धर्म के समर्थन की भावना से ख़ाली होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य साबित किया जाए।
विश्व के चार प्रमुख धर्म
इस संक्षिप्त पुस्तक में विश्व के सभी छोटे-बड़े धर्मों की युद्ध-संबंधी शिक्षाओं की समीक्षा करना संभव नहीं है। इस प्रकार का कवरेज न तो आसान है और न ही आवश्यक है। आम तौर पर धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन केवल उन्हीं धर्मों तक सीमित होते हैं जिन्हें उनके अनुयायियों की संख्या, उनके प्रभावों के फैलाव और उनके अतीत और वर्तमान की महानता के कारण दुनिया के प्रमुख धर्म माना जाता है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम अपनी बहस को चार प्रमुख धर्मों तक सीमित रखेंगे, अर्थात् हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म।
युद्ध के मुद्दे पर इन चारों धर्मों को दो पक्षों में विभाजित किया गया है। एक पक्ष वह है जिसने युद्ध को उचित ठहराया। इसमें हिंदू धर्म और यहूदी धर्म शामिल हैं। दूसरा पक्ष वह है जिसमें युद्ध न्यायसंगत नहीं है, इसमें बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म शामिल हैं, हम अपनी चर्चा पहले पक्ष से शुरू करेंगे।
(1) हिन्दू धर्म
इस धर्म की चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति को सबसे पहले इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि हिंदू धर्म किसे कहा जाए। हिंदुवाद इस अर्थ में कोई धर्म ही नहीं है जिसमें आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्म के लिए अनिवार्य है कि उसकी एक केंद्रीय आस्था हो, जिस पर उसकी आधारशिला रखी गई हो। मगर हिंदू धर्म में हमें ऐसी कोई केंद्रीय आस्था नहीं मिलती। विभिन्न वर्ग और समूह जिनकी मान्यताएं, कर्मकांड, पूजा-पाठ और ग्रंथ आदि एक-दूसरे से सर्वथा पृथक हैं, उनमें सम्मिलित हैं और वे सभी हिन्दू कहलाते हैं। इसलिए, जब हम किसी मुद्दे पर हिंदू धर्म का पक्ष मालूम करते हैं, तो हमें यह तय करने में बड़ी कठिनाई होती है कि उसके गुटों में से किसको सम्बोधित किया जाए।
हिंदू धर्म को परिभाषित करने में शोधकर्ताओं ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया है, कुछ का कहना है कि “हिंदू धर्म वह है जो एक हिंदू करता है।” (An Introduction to the Study of Hinduism, Guru Prasad Sen, p.9) कुछ का कहना है कि यह उन मान्यताओं, परंपराओं, पूजापद्धतियों और परिवर्धनों का संग्रह है जिनकी पुष्टि ब्राह्मणों के आदेशों और पवित्र ग्रंथों से होती है और जिन्हें ब्राह्मणों की शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया है। (Religious Systems of the World, Sir Alfred Comyn Lyall, 114) और कोई कहता है कि भारत के सभी लोग जो इस्लाम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म और किसी अन्य धर्म से संबंधित नहीं हैं और जिनकी पूजापद्धति एकेश्वरवाद से लेकर मूर्तिपूजा तक विस्तृत हो और जिनके मूल धार्मिक उपदेश संस्कृत में लिखे हों, वे हिंदू हैं। (Census Report Baroda, 1901 p.120)
हिंदुओं के आधुनिक धार्मिक रुझान ने इस समस्या को कुछ हद तक सरल कर दिया है। हालांकि धर्मों और पंथों के बीच विभेद अब भी बना हुआ है, लेकिन हिंदुओं में कुछ विशिष्ट ग्रंथों पर अपनी धार्मिक भक्ति को केंद्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उनमें से एक विशाल बहुमत ने उन ग्रंथों को अपने धर्म की आधारशिला के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये ग्रंथ तीन हैं। चार वेद, गीता और मनुस्मृति। यहां हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसका स्रोत ये ही तीन ग्रंथ होंगे।
हिंदू धर्म के तीन काल
ये तीन पुस्तकें तीन अलग-अलग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं और युद्ध के विषय पर हिंदू धर्म के तीन पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं।
वेदों का संबंध उस काल से है जब आर्यों ने मध्य एशिया से निकल कर भारत पर आक्रमण किया था और इस देश के मूल निवासियों के साथ युद्ध किया, जो रंग, जाति और धर्म में उनसे बिल्कुल अलग थे। उस युद्ध में अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ विदेशी आक्रमणकारियों की भावनाएं क्या थीं? उन्हें वे किस दृष्टि से देखते थे? उनके साथ झगड़े का कारण क्या था? उनके विरुद्ध युद्ध के उद्देश्य क्या थे? और वे उनके साथ किस तरह का मामला करना पसंद करते थे? वेदों के श्लोक इन प्रश्नों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।
गीता उस काल का ग्रंथ है जब आर्यों ने उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और आर्यों के दो शक्तिशाली राजवंशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। यह पुस्तक हमें कृष्णजी जैसे धर्मगुरू के माध्यम से युद्ध पर हिंदू दार्शनिक विचारों की जानकारी देती है।
मनुस्मृति उस काल के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क़ानूनों का संग्रह है जब भारत पूरी तरह आर्यावर्त बन चुका था, अनार्य समुदायों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और इस देश में आर्यों की सभ्यता अपने चरम पर थी। इस किताब में हमें युद्ध के नियमों एवं सिद्धांतों और विजित राष्ट्रों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं।
वेदों में युद्ध की शिक्षा
वेद शब्द अलग-अलग नामों से जानी जाने वाली चार किताबों को संदर्भित करता है। उनमें से सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। फिर क्रमश: यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उनके मन्त्रों को विषयों के आधार पर वर्गीकृत करना कठिन है, क्योंकि प्राय: ऐसा होता है कि एक ही मन्त्र में अनेक विषय आ जाते हैं। अतः हम प्रत्येक ग्रन्थ के उन मन्त्रों को पृथक-पृथक उद्धृत करेंगे, जो युद्ध से किसी तरह जुड़ी हों।
ऋग्वेद
ऋग्वेद के जिन मंत्रों में युद्ध का विषय मिलता है वे इस प्रकार हैं:
(स्वामी दयानन्द सरस्वती के संस्कृत भाष्य के आधार पर)
एन्द्र सानसिं रयिं सजित्वानं सदासहम्। वर्षिष्ठमूतये भर॥
नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहै। त्वोतासो न्यर्वता॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 8; मन्त्र » 1,2)
हे (इन्द्र) परमेश्वर! आप कृपा करके हमारी (ऊतये) रक्षा पुष्टि और सब सुखों की प्राप्ति के लिये (वर्षिष्ठम्) जो अच्छी प्रकार वृद्धि करनेवाला (सानसिम्) निरन्तर सेवने के योग्य (सदासहम्) दुष्ट शत्रु तथा हानि वा दुःखों के सहने का मुख्य हेतु (सजित्वानम्) और तुल्य शत्रुओं का जितानेवाला (रयिम्) धन है, उस को (आभर) अच्छी प्रकार दीजिये॥१॥
हे जगदीश्वर! (त्वोतासः) आप के सकाश से रक्षा को प्राप्त हुए हम लोग (येन) जिस पूर्वोक्त धन से (मुष्टिहत्यया) बाहुयुद्ध और (अर्वता) अश्व आदि सेना की सामग्री से (निवृत्रा) निश्चित शत्रुओं को (निरुणधामहै) रोकें अर्थात् उनको निर्बल कर सकें, ऐसे उत्तम धन का दान हम लोगों के लिये कृपा से दीजिये॥२॥
घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 12; मन्त्र » 5)
(घृताहवन) जिसमें घी तथा जल क्रियासिद्ध होने के लिये छोड़ा जाता और जो अपने (दीदिवः) शुभ गुणों से पदार्थों को प्रकाश करनेवाला है, (त्वम्) वह (अग्ने) अग्नि (रक्षस्विनः) जिन समूहों में राक्षस अर्थात् दुष्टस्वभाववाले और निन्दा के भरे हुए मनुष्य विद्यमान हैं, तथा जो कि (रिषतः) हिंसा के हेतु दोष और शत्रु हैं, उनका (प्रति दह स्म) अनेक प्रकार से विनाश करता है, हम लोगों को चाहिये कि उस अग्नि को कार्यों में नित्य संयुक्त करें॥५॥
तयोरिदवसा वयं सनेम नि च धीमहि। स्यादुत प्ररेचनम्॥
इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधसे। अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 17; मन्त्र » 6,7)
हम लोग जिन इन्द्र और वरुण के (अवसा) गुणज्ञान वा उनके उपकार करने से (इत्) ही जिन सुख और उत्तम धनों को (सनेम) सेवन करें (तयोः) उनके निमित्त से (च) और उनसे पाये हुए असंख्यात धन को (निधीमहि) स्थापित करें अर्थात् कोश आदि उत्तम स्थानों में भरें, और जिन धनों से हमारा (प्रचेरनम्) अच्छी प्रकार अत्यन्त खरच (उत) भी (स्यात्) सिद्ध हो॥६॥ जो (इन्द्रावरुणा) पूर्वोक्त इन्द्र और वरुण अच्छी प्रकार क्रिया कुशलता में प्रयोग किये हुए (अस्मान्) हम लोगों को (सुजिग्युषः) उत्तम विजययुक्त (कृतम्) करते हैं, (वाम्) उन इन्द्र और वरुण को (चित्राय) जो कि आश्चर्य्यरूप राज्य, सेना, नौकर, पुत्र, मित्र, सोना, रत्न, हाथी, घोड़े आदि पदार्थों से भरा हुआ (राधसे) जिससे उत्तम-उत्तम सुखों को सिद्ध करते हैं, उस सुख के लिये (अहम्) मैं मनुष्य (हुवे) ग्रहण करता हूँ॥७॥
सर्वं परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम्।
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 29; मन्त्र » 7)
हे (तुविमघ) अनन्त बलरूप धनयुक्त (इन्द्र) सब शत्रुओं के विनाश करनेवाले जगदीश्वर आप जो (नः) हमारे (सहस्रेषु) अनेक (शुभ्रिषु) शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार वा (गोषु) पृथिवी के राज्य आदि व्यवहार तथा (अश्वेषु) घोड़े आदि सेना के अङ्गों में विनाश का करानेवाला व्यवहार हो, उस (परिक्रोशम्) सब प्रकार से रुलानेवाले व्यवहार को (जहि) विनष्ट कीजिये तथा जो (नः) हमारा शत्रु हो (कृकदाश्वम्) उस दुःख देनेवाले को भी (जम्भय) विनाश को प्राप्त कीजिये। इस रीति से (तु) फिर (नः) हम लोगों को (आशंसय) शत्रुओं से पृथक् कर सुखयुक्त कीजिये॥७॥
वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासदव्रतान्।
शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 51; मन्त्र » 8)
हे मनुष्य ! तू (बर्हिष्मते) उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करनेवाले व्यवहार की सिद्धि के लिये (आर्य्यान्) सर्वोपकारक धार्मिक विद्वान् मनुष्यों को (विजानीहि) जान और (ये) जो (दस्यवः) परपीड़ा करनेवाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य हैं, उनको जान कर (बर्हिष्मते) धर्म की सिद्धि के लिये (रन्धय) मार और उन (अव्रतान्) सत्यभाषणादि धर्मरहित मनुष्यों को (शासत्) शिक्षा करते हुए (यजमानस्य) यज्ञ के कर्ता का (चोदिता) प्रेरणाकर्त्ता और (शाकी) उत्तम शक्तियुक्त सामर्थ्य को (भव) सिद्ध कर, जिससे (ते) तेरे उपदेश वा सङ्ग से (सधमादेषु) सुखों के साथ वर्त्तमान स्थानों में (ता) उन (विश्वा) सब कर्मों को सिद्ध करने की (इत्) ही मैं (चाकन) इच्छा करता हूँ ॥ ८॥
डॉ. राजेंद्र लाल मित्रा ने अपनी किताब (इंडो आर्यन्स) में यह साबित करने की कोशिश की है कि दस्यु स्वयं आर्यों की दुष्ट जनजातियां हैं (खंड I: पृ. 210) लेकिन स्वयं वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य आक्रमणकर्ता इस शब्द का प्रयोग भारत के उन मूल निवासियों के लिए किया करते थे जिनके साथ वे युद्धरत्त थे। Ralph Thomas Hotchkin Griffith (1826–1906) लिखते हैं:
“इस नाम (दस्यु) का प्रयोग प्राय: स्वदेशी लोगों के लिए किया जाता है जिन्होंने आर्यों के प्रवास का विरोध किया था, बाद में यह शब्द उन सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो वेद की पूजा और कुछ विशेष ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का अभ्यास नहीं करते थे।” (अथर्ववेद का अनुवाद: खंड, पृ. 9)
प्रोफेसर ब्लूमफील्ड लिखते हैं:
“अज्ञात काल में जो आधुनिक अनुमानों के अनुसार 1500 ई.पू. में शुरू हुआ था, मगर हो सकता है कि वह और भी प्राचीन काल से शुरू हुआ हो, आर्य जनजातियों ने ईरान की ऊंचाई से, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंकला के उत्तर में हैं, से पलायन कर उत्तर-पश्चिमी भारत, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की भूमि में बसना शुरू किया। देश के मूल ग़ैर-आर्यन निवासी, जिन्हें आर्यों से अलग करने के लिए दस्यु कहा जाता था, आसानी से पराजित हो गए।” (Encyclopaedia of Religions, Vol. VIII, p.107)
प्रोफेसर मैकडॉनेल लिखते हैं:
“ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्दों का प्रयोग प्राय: काले रंग के प्राचीन निवासियों के लिए किया गया है, जिन पर आर्यों ने विजय प्राप्त की थी।” (Encyclopaedia of Religions, Vol. XII, p.610)
विलियम क्रुक लिखते हैं:
“महान देवता अपने पुजारियों के उदार संरक्षक हैं, जो दस्यु या गहरे रंग के मूल निवासियों के ख़िलाफ़ युद्ध में हिन्दू-आर्यों का नेतृत्व करते हैं।” (Encyclopaedia of Religions, Vol. VI, p.691)
एभिर्द्युभिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अमतिं गोभिरश्विना।
इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभिर्युतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः।
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 53; मन्त्र » 4,5)
हम लोग जो (अमतिम्) विज्ञान वा सुख से अविद्या दरिद्रता तथा सुन्दर रूप को (निरुन्धानः) निरोध वा ग्रहण करता हुआ (सुमनाः) उत्तम विज्ञानयुक्त सभाध्यक्ष है, उसकी प्राप्ति कर उसके सहाय वा (एभिः) इन (द्युभिः) प्रकाशयुक्त द्रव्य (एभिः) इन (इन्दुभिः) आह्लादकारक गुण वा पदार्थ इन (गोभिः) प्रशंसनीय गौ पृथिवी (अश्विना) अग्नि, जल, सूर्य्य, चन्द्र आदि (इषा) इच्छा वा अन्नादि (इन्दुभिः) सोमरसादि पेयों (इन्द्रेण) बिजुली और उसके रचे हुए विदारण करनेवाले शस्त्र से (दस्युम्) बल से दूसरे के धन को लेनेवाले दुष्ट को (दरयन्तः) विदारण करते हुए (युतद्वेषसः) द्वेष से अलग होनेवाले शत्रुओं के साथ युद्ध को सुख से (समारभेमहि) आरम्भ करें ॥ ४ ॥ हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग आप के सहाय से (सम्राया) उत्तम राज्यलक्ष्मी (समिषा) धर्म की इच्छा वा अन्नादि (अभिद्युभिः) विद्या व्यवहार और प्रकाशयुक्त (पुरुश्चन्द्रैः) बहुत आह्लादकारक सुवर्ण और उत्तम चांदी आदि धातु (सं वाजेभिः) विज्ञानादि गुण वा संग्राम तथा (प्रमत्या) उत्तम मतियुक्त (देव्या) दिव्यगुण सहित विद्या से युक्त सेना से (गोअग्रया) श्रेष्ठ इन्द्रिय गौ और पृथिवी से युक्त (वीरशुष्मया) शूरवीर योद्धाओं के बल से युक्त (अश्ववत्या) प्रशंसनीय वेग, बलयुक्त घोड़ेवाली सेना के साथ वर्त्तमान होके शत्रुओं के साथ (संरभेमहि) अच्छे प्रकार संग्राम को करें, इस सब कार्य्य को करके लौकिक और पारमार्थिक सुखों को (रभेमहि) सिद्ध करें ॥ ५ ॥
स शेवृधमधि धा द्युम्नमस्मे महि क्षत्रं जनाषाळिन्द्र तव्यम्।
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीन्राये च नः स्वपत्या इषे धाः ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 54; मन्त्र » 11)
पदार्थ - हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्यसम्पादक सभाध्यक्ष ! जो (जनाषाट्) जनों को सहन करने हारे आप (अस्मे) हम लोगों के लिये (शेवृधम्) सुख (तव्यम्) बलयुक्त (महि) महासुखदायक पूजनीय (क्षत्रम्) राज्य को (अधि) (धाः) अच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर (मघोनः) प्रशंसनीय धन वा (नः) हम लोगों की (रक्ष) रक्षा (च) और (सूरीन्) बुद्धिमान् विद्वानों की (पाहि) रक्षा कीजिये (च) और (नः) हम लोगों के (राये) धन (च) और (स्वपत्यै) उत्तम अपत्ययुक्त (इषे) इष्टरूप राजलक्ष्मी के लिये (द्युम्नम्) कीर्त्तिकारक धन को (धाः) धारण करते हो (सः) वह आप हम लोगों से सत्कार योग्य क्यों न होवें ॥ ११ ॥
तमित्सुहव्यमङ्गिरः सुदेवं सहसो यहो। जना आहुः सुबर्हिषम् ॥
आ च वहासि ताँ इह देवाँ उप प्रशस्तये। हव्या सुश्चन्द्र वीतये ॥
न योरुपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथस्य कच्चन। यदग्ने यासि दूत्यम् ॥
त्वोतो वाज्यह्रयोऽभि पूर्वस्मादपरः। प्र दाश्वाँ अग्ने अस्थात् ॥
उत द्युमत्सुवीर्यं बृहदग्ने विवाससि। देवेभ्यो देव दाशुषे ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 74; मन्त्र » 5-9)
हे (अङ्गिरः) अङ्गों के रसरूप (सहसः) बल के (यहो) पुत्ररूप विद्वान् मनुष्य! जिस तुझको बिजुली के तुल्य (सुदेवम्) दिव्यगुणों के देने (सुबर्हिषम्) विज्ञानयुक्त (सुहव्यम्) उत्तम ग्रहण करनेवाले आपको (जनाः) विद्वान् लोग (आहुः) कहते हैं (तम्) उसको (इत्) ही हम लोग सेवन करें ॥ ५ ॥ हे (सुश्चन्द्र) अच्छे आनन्द देनेवाले विद्वान् ! आप (इह) इस संसार में (प्रशस्तये) प्रशंसा (च) और (वीतये) सुखों की प्राप्ति के लिये जिन (हव्या) ग्रहण के योग्य (देवान्) दिव्य गुणों वा विद्वानों को (उपावहासि) समीप में सब प्रकार प्राप्त हों (तान्) उन आप को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्या से प्रकाशित विद्वान् ! आप जैसे (उपब्दि) अत्यन्त शब्द करने (अश्व्यः) शीघ्र चलनेवाले यानों में अत्यन्त वेगकारक (यत्) जिस अग्नियुक्त और (योः) चलने-चलानेवाले (रथस्य) विमानादि यानसमूह के बीच स्थिर होके (दूत्यम्) दूत के तुल्य अपने कर्म को (यासि) प्राप्त होते हो, मैं उस अग्नि के समीप और शब्दों को (कच्चन) कभी (न) नहीं (शृण्वे) सुनता किन्तु प्राप्त होता हूँ, तू भी नहीं सुन सकता, परन्तु प्राप्त हो सकता है ॥ ७ ॥ हे (अग्ने) विद्यायुक्त ! जैसे (अह्रयः) शीघ्रयान मार्गों को प्राप्त करानेवाले अग्नि आदि (अपरः) और भिन्न देश वा भिन्न कारीगर (त्वोतः) आपसे संगम को प्राप्त हुआ (वाजी) प्रशंसा के योग्य वेगवाला (दाश्वान्) दाता (पूर्वस्मात्) पहले स्थान से (अभि) सन्मुख (प्रास्थात्) देशान्तर को चलानेवाला होता है, वैसे अन्य मन आदि पदार्थ भी हैं, ऐसा तू जान ॥ ८ ॥ हे (देव) दिव्य गुण, कर्म्म और स्वभाववाला (अग्ने) अग्निवत् प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान् ! तू (दाशुषे) देने के स्वभाववाले कार्य्यों के अध्यक्ष (उत) अथवा (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (द्युमत्) अच्छे प्रकाशवाले (बृहत्) बड़े (सुवीर्य्यम्) अच्छे पराक्रम को (विवासति) सेवन करता है, वैसे हम भी उसका सेवन करें ॥ ९ ॥
गोरी चमड़ी वाले लोग गोरी चमड़ी वाले आर्य क़बीले हैं जिन्होंने नदी के उस पार से भारत पर आक्रमण किया था। इसके विपरीत, भारत के मूल निवासी काले थे (ग्रीफिथ का अंग्रेज़ी अनुवाद, ऋग्वेद, खंड I, पृष्ठ 130)।
दस्यूञ्छिम्यूँश्च पुरुहूत एवैर्हत्वा पृथिव्यां शर्वा नि बर्हीत्।
सनत्क्षेत्रं सखिभिः श्वित्न्येभि: सनत्सूर्यं सनदपः सुवज्र: ॥
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिह्वृताः सनुयाम वाजम्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 100; मन्त्र » 18,19)
(सुवज्रः) जिसका श्रेष्ठ अस्त्र और शस्त्रों का समूह और (पुरुहूतः) बहुतों ने सत्कार किया हो वह (शर्वा) समस्त दुःखों का विनाश करनेवाला सभा आदि का अधीश (श्वित्न्येभिः) श्वेत अर्थात् स्वच्छ तेजस्वी (सखिभिः) मित्रों के साथ और (एवैः) प्रशंसित ज्ञान वा कर्मों के साथ (दस्यून्) डाकुओं को (हत्वा) अच्छे प्रकार मार (शिम्यून्) शान्त धार्मिक सज्जनों (च) और भृत्य आदि को (सनत्) पाले, दुःखों को (नि, बर्हीत्) दूर करे, जो (पृथिव्याम्) अपने राज्य से युक्त भूमि में (क्षेत्रम्) अपने निवासस्थान (सूर्यम्) सूर्यलोक, प्राण (अपः) और जलों को (सनत्) सेवे, वह सबको (सनत्) सदा सेवने के योग्य होवे ॥ १८ ॥ जो (इन्द्रः) प्रशंसित विद्या और ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वान् (नः) हम लोगों के लिये (विश्वाहा) सब दिनों (अधिवक्ता) अधिक-अधिक उपदेश करनेवाला (अस्तु) हो, उससे (अपरिह्वृताः) सब प्रकार कुटिलता को छोड़े हुए हमलोग जिस (वाजम्) विशेष ज्ञान को (सनुयाम) दूसरे को देवें और आप सेवन करे (नः) हमारे (तत्) उस विज्ञान को (मित्रः) मित्र (वरुणः) श्रेष्ठ सज्जन (अदितिः) अन्तरिक्ष (सिन्धुः) समुद्र नदी (पृथिवी) भूमि (उत) और (द्यौः) सूर्य्य आदि प्रकाशयुक्त लोकों का प्रकाश (मामहन्ताम्) मान से बढ़ावें ॥ १९ ॥
भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषे नृतो।
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत्। महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा ॥
इन्द्र: समत्सु यजमानमार्यं प्रावद्विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीळ्हेष्वाजिषु।
मनवे शासदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्। दक्षन्न विश्वं ततृषाणमोषति न्यर्शसानमोषति ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 130; मन्त्र » 7,8)
हे (नृतो) अपने अङ्गों को युद्ध आदि में चलाने वा (नृतो) विद्या की प्राप्ति के लिये अपने शरीर की चेष्टा करने (इन्द्र) और दुष्टों का विनाश करनेवाले ! जो आप (वज्रेण) शस्त्र वा उपदेश से शत्रुओं की (नवतिम्) नब्बे (पुरः) नगरियों को (भिनत्) विदारते नष्ट-भ्रष्ट करते वा (महि) बड़प्पन पाये हुए सत्कारयुक्त (दिवोदासाय) चहीते पदार्थ को अच्छे प्रकार देनेवाले और (दाशुषे) विद्यादान किये हुए (पूरवे) पूरे साधनों से युक्त मनुष्य के लिये सुख को धारण करते तथा (अतिथिग्वाय) अतिथियों को प्राप्त होने और (दाशुषे) दान करनेवाले के लिये (उग्रः) तीक्ष्ण स्वभाव अर्थात् प्रचण्ड प्रतापवान् सूर्य (गिरेः) पर्वत के आगे (शम्बरम्) मेघ
को जैसे वैसे (ओजसा) अपने पराक्रम से (महः) बड़े-बड़े (धनानि) धन आदि पदार्थों के (दयमानः) देनेवाले (ओजसा) पराक्रम से (विश्वा) समस्त (धनानि) धनों को (अवाभरत्) धारण करते सो आप किञ्चित् भी दुःख को कैसे प्राप्त होवें ॥ ७ ॥ जो (शतमूतिः) अर्थात् जिससे असंख्यात रक्षा होती वह (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् राजा (स्वर्मीढेषु) जिनमें सुख सिञ्चन किया जाता उन (आजिषु) प्राप्त हुए (आजिषु) संग्रामों में धार्मिक शूरवीरों के समान (विश्वेषु) समग्र (समत्सु) संग्राम में (यजमानम्) अभय के देनेवाले (आर्यम्) उत्तम गुण, कर्म, स्वभाववाले पुरुष को (प्रावत्) अच्छे प्रकार पाले वा (मनवे) विचारशील धार्मिक मनुष्य की रक्षा के लिये (अव्रतान्) दुष्ट आचरण करनेवाले डाकुओं को (शासत्) शिक्षा देवे और इनकी (त्वचम्) सम्बन्ध करनेवाली खाल को (कृष्णाम्) खैंचता हुआ (अरन्धयत्) नष्ट करे वा अग्नि जैसे (विश्वम्) सब पदार्थ मात्र को (दक्षन्) जलावे और (ततृषाणम्) पियासे प्राणी को (ओषति) दाहे अति जलन देवे (न) वैसे (अर्शसानम्) प्राप्त हुए शत्रुगण को (न्योषति) निरन्तर जलावे, वही चक्रवर्त्ति राज्य करने योग्य होता है ॥ ८ ॥
त्वया वयं मघवन्पूर्व्ये धन इन्द्रत्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः।
नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधि वोचा नु सुन्वते अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा भरे कृतं वाजयन्तो भरे कृतम् ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 132; मन्त्र » 1)
हे (मघवन्) परम प्रशंसित बहुत धनवाले (इन्द्रत्वोताः) अतिउत्तम ऐश्वर्ययुक्त जो आप उन्होंने पाले हुए (वयम्) हम लोग (त्वया) आप के साथ (पूर्व्ये) अगले महाशयों ने किये (धने) धन के निमित्त (पृतन्यतः) मनुष्यों के समान आचरण करते हुए मनुष्यों को (सासह्याम) निरन्तर सहें (वनुष्यतः) और सेवन करनेवालों का (वनुयाम) सेवन करें तथा (भरे) रक्षा में (कृतम्) प्रसिद्ध हुए को (वाजयन्तः) समझाते हुए हम लोग (अस्मिन्) इस (यज्ञे) यज्ञ में तथा (भरे) संग्राम में (कृतम्) उत्पन्न हुए व्यवहार को (विचयेम) विशेष कर खोजें और (नेदिष्ठे) अति निकट (अस्मिन्) इस (अहनि) आज के दिन (सुन्वते) व्यवहारों की सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (नु) शीघ्र (अधिवोच) सबके उपरान्त करो ॥१ ॥
सं यज्जनान्क्रतुभि: शूर ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यव: प्र यक्षन्त श्रवस्यव:।
तस्मा आयु: प्रजावदिद्बाधे अर्चन्त्योजसा। इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतय: ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 132; मन्त्र » 5)
हे विद्वानो ! (श्रवस्यवः) अपने को सुनने में चाहना करनेवालों के समान वर्त्तमान (श्रवस्यवः) अपने सुनने की इच्छा करनेवाले तुम जैसे (क्रतुभिः) बुद्धि वा कर्मों से (यत्) जिन (जनान्) धार्मिक जनों को (हिते) सुख करनेहारे (धने) धन के निमित्त (तरुषन्त) पार करो उद्धार करो और (प्रयक्षन्त) दुष्टों को दण्ड देओ और जो (शूरः) निर्भय शूरवीर पुरुष (समीक्षयत्) ज्ञान करावे व्यवहार को दर्शावे (तस्मै) उसके लिये (प्रजावत्) जिसमें बहुत सन्तान विद्यमान वह (आयुः) आयुर्दा हो। हे उत्तम विचारशील पुरुषो ! तुम (धीतयः) धारण करते हुओं के (न) समान (धीतयः) धारणा करनेवाले होते हुए परमऐश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर में (ओक्यम्) घरों में श्रेष्ठ व्यवहार उसको सिद्ध कर (देवान्) विद्वानों को (अच्छ) अच्छा (दिधिषन्त) उपदेश करते समझाते हो वे आप (बाधे) दुष्ट व्यवहारों को बाधा के लिये (ओजसा) पराक्रम से (अर्चन्ति) सत्कार करते हुओं के समान कष्ट में (इत्) ही रक्षा करो ॥ ५ ॥
त्वमस्माकमिन्द्र विश्वध स्या अवृकतमो नरां नृपाता।
स नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 174; मन्त्र » 10)
हे (इन्द्र) सुख देनेवाले ! (त्वम्) आप (अस्माकम्) हमारे बीच (विश्वध) सब प्रकार से (नराम्) मनुष्यों में (नृपाता) मनुष्यों की रक्षा करनेवाले अर्थात् प्रजाजनों की पालना करनेवाले और (अवृकतमः) जिनके सम्बन्ध में चोरजन नहीं ऐसे (स्याः) हूजिये तथा (सः) सो आप (नः) हमारे (विश्वासाम्) समस्त (स्पृधाम्) युद्ध की क्रियाओं के (सहोदाः) बल देनेवाले हूजिये जिससे हम लोग (जीरदानुम्) जीव के रूप को (वृजनम्) धर्मयुक्त मार्ग को और (इषम्) शास्त्रविज्ञान को (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ १० ॥
त्वं हि शूर: सनिता चोदयो मनुषो रथम्।
सहावान्दस्युमव्रतमोष: पात्रं न शोचिषा ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 175; मन्त्र » 3)
हे सेनापति ! (हि) जिस कारण (शूरः) शूरवीर निडर (सनिता) सेना को संविभाग करने अर्थात् पद्मादि व्यूह रचना से बाँटनेवाले (त्वम्) आप (मनुषः) मनुष्यों और (रथम्) युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रथ को (चोदयः) प्रेरणा दें अर्थात् युद्ध समय में आगे को बढ़ावें और (सहावान्) बलवान् आप (शोचिषा) दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे (पात्रम्) काष्ठ आदि के पात्र को (न) वैसे (अव्रतम्) दुश्शील दुराचारी (दस्युम्) हठ कर पराये धन को हरनेवाले दुष्टजन को (ओषः) जलाओ इससे मान्यभागी होओ ॥ ३ ॥
इमं नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुप ब्रुवे।
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मृळतु पुलुकामो हि मर्त्य: ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 179; मन्त्र » 5)
पदार्थ - मैं (यत्) जिस (इमम्) इस (हृत्सु) हृदयों में (पीतम्) पिये हुए (सोमम्) ओषधियों के रस के (उप, ब्रुवे) उपदेशपूर्वक कहता हूँ उसको (पुलुकामः) बहुत कामनावाला (मर्त्यः) पुरुष (हि) ही (सुमृलतु) सुखसंयुक्त करे अर्थात् अपने सुख में उसका संयोग करे। जिस (आगः) अपराध को हम लोग (चकृम) करें (तत्) उसको (नु) शीघ्र (सीम्) सब ओर से (अन्तिमः) समीप से सभी जन छोड़ें अर्थात् क्षमा करें ॥ ५ ॥
सनेम ये त ऊतिभिस्तरन्तो विश्वाः स्पृध आर्येण दस्यून्।
अस्मभ्यं तत्त्वाष्ट्रं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य त्रिताय॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 2; सूक्त » 11; मन्त्र » 19)
हे सेनापति! (ये) जो (ते) आपकी (ऊतिभिः) रक्षा आदि कामों की करनेवाली सेनाओं से (विश्वाः) समस्त (स्पृधः) स्पर्द्धा करनेवालों को (तरन्तः) उल्लंघन करते हुए हम लोग (त्रिताय) त्रिविध अर्थात् शारीरिक वाचिक और मानसिक सुख जिसको प्राप्त उसके लिये (आर्य्येण) उत्तम विद्या और धर्म सामर्थ्य के साथ (दस्यून्) डाकुओं को जीतें जो (साख्यस्य) मित्रपन वा मित्रकर्म करने का (विश्वरूपम्) विविध स्वरूप (त्वाष्ट्रम्) प्रकाशमान का रचा हुआ है उसको (सनेम) अलग-अलग करें (तत्) उसको आप (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये सिद्ध करो और डाकुओं को (अरन्धयः) नष्ट करो ॥१९॥
वनस्पतिरवसृजन्नुप स्थादग्निर्हविः सूदयाति प्र धीभिः।
त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोप हव्यम्॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 2; सूक्त » 3; मन्त्र » 10)
हे विद्वान्! जैसे (धीभिः) कर्मों के साथ वर्त्तमान (वनस्पतिः) वरगद आदि (अवसृजन्) फलादिकों का त्याग करता हुआ (उपस्थात्) उपस्थित होता है वा (अग्निः) अग्नि (त्रिधा) तीन प्रकार के (समक्तम्) समूह को प्राप्त हुए (हविः) होमने योग्य द्रव्य को (सूदयाति) प्राणिमात्र के सुख के लिये कण-कण करके पहुँचाता है, वैसे (शमिता) शान्ति करनेवाला (दैव्यः) विद्वानों में प्राप्त हुए (प्रजानन्) उत्तम ज्ञान को प्राप्त होते हुए आप (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये (उपहव्यम्) समीप में ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (प्रनयतु) प्राप्त कीजिये ॥१०॥
पुरू यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकर्थोर्वरासु युध्यन्।
ततक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे वृषा समत्सु दासस्य नाम चित् ॥४॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 5; सूक्त » 33; मन्त्र » 4)
हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त (वृषा) बलिष्ठ होते हुए आप (ते) आपके (यत्) जो (पुरु) बहुत (उक्था) प्रशंसित कर्म्म (गवे) गौ आदि पशुओं के हित के लिये (सन्ति) हैं उनको (उर्वरासु) भूमियों में और (समत्सु) सङ्ग्रामों में (युध्यन्) युद्ध करते हुए (चकर्थ) करें और शत्रुओं को (ततक्षे) सूक्ष्म अर्थात् निर्बल करते हो और (सूर्य्याय) सूर्य्य के सदृश वर्त्तमान के लिये (चित्) भी (स्वे) अपने (ओकसि) गृह में (दासस्य) दास के (चित्) निश्चित (नाम) नाम को प्रकट कीजिये ॥४॥
ससानात्याँ उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्।
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्प्रार्यं वर्णमावत्॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 3; सूक्त » 34; मन्त्र » 9)
वह (इन्द्रः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त राजा वा मन्त्रियों का समूह (अत्यान्) उत्तम शिक्षा से घोड़ों के (ससान) विभाग को और (सूर्यम्) सूर्य के सदृश प्रतापयुक्त वीर पुरुष को (ससान) अलग करै (पुरुभोजसम्) बहुतों का पालन वा बहुतों को नहीं भोजन देनेवाले पुरुष की (गाम्) वाणी वा भूमि का (उत) और (हिरण्ययम्) सुवर्ण आदि पदार्थों का (ससान) विभाग करै वह पुरुष (दस्यून्) साहस कर्म करनेवाले चोर आदि का (हत्वी) नाश करके (आर्य्यम्) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त धार्मिक (वर्णम्) स्वीकार करने योग्य पुरुष की (प्र) (आवत्) रक्षा करै ॥९॥
यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्।
तमजरेभिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान् ॥४॥
यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरर्केभिः सूनो सहसो ददाशत्।
स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा वि भाति ॥५॥
स तत्कृधीषितस्तूयमग्ने स्पृधो बाधस्व सहसा सहस्वान्।
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म ॥६॥
अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्याम रयिं रयिवः सुवीरम्।
अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम द्युम्नमजराजरं ते ॥७॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 5; मन्त्र » 4,7)
हे (तपिष्ठ) अत्यन्त तप करनेवाले और (मित्रमहः) बड़े मित्रों से युक्त (अग्ने) विद्वन् ! (यः) जो (सनुत्यः) निश्चित अन्तर्हित अर्थात् मध्य के सिद्धान्तों में प्रकट हुआ अथवा श्रेष्ठ (नः) हम लोगों का (अभिदासत्) चारों ओर से नाश करता है और (यः) जो (अन्तरः) भिन्न हम लोगों से (वनुष्यात्) याचना करे (तम्) उसको (अजरेभिः) वृद्धावस्था से रहित (वृषभिः) बलिष्ठ युवा (तव) आपके (स्वैः) अपने जनों के साथ (तपा) तपयुक्त करो वा तपस्वी हो ओ।और (तपसा) ब्रह्मचर्य और प्राणायामादि कर्म्म से (तपस्वान्) बहुत तपयुक्त हूजिये ॥४॥
हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र और (अमृत) मरणधर्म्म से रहित ! (यः) जो (यज्ञेन) विद्वानों के सत्कारनामक यज्ञ और (समिधा) सत्य के प्रकाशक वा ईंधन से तथा (यः) जो (अर्केभिः) आदर करने योग्य और (उक्थैः) कहने के योग्य पदार्थों से (ते) आपके लिये (ददाशत्) देता है (सः) वह (मर्त्येषु) मनुष्यों में (प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान् (राया) धन (द्युम्नेन) यश और (श्रवसा) अन्न वा श्रवण से (वि, भाति) प्रकाशित होता है, इस प्रकार विशेष करके जानो ॥५॥ हे (अग्ने) अग्नि के सदृश प्रतापयुक्त ! (यत्) जो आप (द्युभिः) प्रकाशमान दिनों से (अक्तः) रात्रि जैसे वैसे (शस्यसे) स्तुति किये जाते हो वह आप (वचोभिः) वचनों से (जरितुः) स्तुति करनेवाले का (घोषि) वाणी जिसमें ऐसा (मन्म) विज्ञान है (तत्) उसका (जुषस्व) सेवन करो (सः) वह (सहस्वान्) सहन करनेवाले आप (सहसा) बल से (स्पृधः) स्पर्धा करते हैं जिनमें उन सङ्गग्रामसेनाओं की (बाधस्व) बाधा करते हो तथा (तूयम्) शीघ्र (इषितः) प्रेरित हुए (तत्) उसको (कृधि) करो ॥६॥ हे (अजर) वृद्धावस्थारहित (रयिवः) बहुत धन और (अग्ने) विद्या से युक्त राजन् ! (तव) आपके (ऊती) रक्षण आदि कर्म्म से हम लोग (तम्) उस (कामम्) मनोरथ को (अश्याम) प्राप्त होवें और (सुवीरम्) उत्तम वीरों की प्राप्ति करनेवाले (रयिम्) धन को (अश्याम) प्राप्त होवें तथा (वाजयन्तः) जानते हुए हम लोग (वाजम्) अन्न आदि को (अभि) सन्मुख (अश्याम) प्राप्त होवें और (ते) आपके (अजरम्) जीर्ण होने से रहित (द्युम्नम्) यश वा धन को (अश्याम) प्राप्त होवें ॥७॥
विशां कविं विश्पतिं शश्वतीनां नितोशनं वृषभं चर्षणीनाम्।
प्रेतीषणिमिषयन्तं पावकं राजन्तमग्निं यजतं रयीणाम् ॥८॥
सो अग्न ईजे शशमे च मर्तो यस्त आनट् समिधा हव्यदातिम्।
य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥९॥
अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यैः।
वेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा ते भद्रायां सुमतौ यतेम ॥१०॥
आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्य१स्तरुत्रः।
बृहद्भिर्वाजैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितरं वि भाहि ॥११॥
नृवद्वसो सदमिद्धेह्यस्मे भूरि तोकाय तनयाय पश्वः।
पूर्वीरिषो बृहतीरारेअघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ॥१२॥
पुरूण्यग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम्।
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते राजनि त्वे ॥१३॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 1; मन्त्र » 8-13)
हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (शश्वतीनाम्) अनादिभूत (विशाम्) प्रजाओं के मध्य में (कविम्) तेजयुक्त दर्शन जिसका ऐसे (विश्पतिम्) प्रजा के पालनेवाले (नितोशनम्) पदार्थों के नाश करनेवाले (वृषभम्) बलिष्ठ और (चर्षणीनाम्) मनुष्यों और (रयीणाम्) धनों और (प्रेतीषणिम्) अच्छे प्रकार से प्राप्त हुओं को प्राप्त होनेवाले (इषयन्तम्) प्राप्त कराते हुए और (यजतम्) प्राप्त होने योग्य (राजन्तम्) प्रकाशित होते हुए (पावकम्) पवित्र करनेवाले (अग्निम्) अग्नि को उत्तम प्रकार कार्य्यों में युक्त करें, वैसे आप लोग भी संप्रयुक्त करो ॥८॥ हे (अग्ने) अग्नि के सदृश वर्त्तमान विद्वन् ! (ते) आप का (यः) जो (मर्त्तः) मनुष्य (समिधा) समिध् से (हव्यदातिम्) हवन करने योग्य वस्तुओं के देनेवाले को (आनट्) व्याप्त होता है, उसको जाननेवाला (सः) वह मैं उसको (ईजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होता और (शशमे) प्रशंसा करता हूँ (च) और (यः) जो (आहुतिम्) आहुति को अर्थात् जो चारों ओर होमी जाती उस सामग्री को (परि) सब प्रकार से (वेदा) जानता है (सः) वह (त्वोतः) आप से रक्षित हुआ (नमोभिः) अन्न आदिकों वा सत्कारों से (विश्वा) सम्पूर्ण (वामा) प्रशंसा करने योग्य कर्म्मों को (इत्) ही (दधते) धारण करता है ॥९॥ हे (सहसः) बलवान् के (सूनो) पुत्र (अग्ने) विद्वज्जन ! जैसे (समिधा) ईंधन आदि के सदृश विद्या और (नमोभिः) अन्न आदिकों से संपूर्ण स्त्रियों को जो धारण करते हैं और जो आहुति को देखकर जानता है और जो (वेदी) जानते हैं सुखों को जिसमें वह होती है, उसका (गीर्भिः) वाणियों और (उक्थैः) कीर्त्तन करने योग्य वचनों से और (हव्यैः) भोजन करने योग्य पदार्थों से (अस्मै) इस (महे) बड़े (ते) आपके लिये (महि) बहुत (आ) सब प्रकार से (विधेम) सत्कार करें, उन वाणियों के सहित आप लोग (उ) भी (उत) और हम भी (ते) आपकी (भद्रायाम्) कल्याणकारिणी (सुमतौ) उत्तम बुद्धि में (यतेम) प्रयत्न करें ॥१०॥ हे (अग्ने) विद्वन् ! (यः) जो अग्नि (भासा) प्रकाश से और (श्रवोभिः) श्रवण आदि वा अन्न आदि से (च) भी (श्रवस्यः) सुनने के योग्य और (तरुत्रः) दुःख से पार करनेवाला (बृहद्भिः) बड़े और (स्थविरेभिः) स्थूल अर्थात् भारी (वाजैः) संग्रामों के सहित वर्त्तमान (रेवद्भिः) बहुत धनों से युक्त जनों के साथ (रोदसी) द्यावापृथिवी को (वि, आ, ततन्थ) विशेष कर सब प्रकार विस्तार करता है तथा (अस्मे) हम लोगों के लिये उस (वितरम्) वितर अर्थात् विविध प्रकार से तरते हैं जिससे उसको (वि, भाहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित कीजिये ॥११॥ हे (वसो) वसनेवाले विद्वज्जन ! आप (अस्मे) हम लोगों में (तोकाय) कन्या और (तनयाय) पुत्र के लिये (पश्वः) पशु गौ आदि को तथा (सदम्) वर्त्तमान होते हैं जिसमें उस गृह और (बृहतीः) बड़ी (पूर्वीः) प्राचीन (आरेअघाः) दूर पाप जिनके उन (इषः) अन्न आदि सामग्रियों को (भूरि) बहुत (धेहि) धारण करिये जिससे (अस्मे) हम लोगों के लिये (इत्) ही (नृवत्) मनुष्यों के सदृश (भद्रा) कल्याणकारक (सौश्रवसानि) उत्तम प्रकार संस्कार से युक्त अन्न में हुए पदार्थ (सन्तु) हों ॥१२॥ हे (अग्ने) विद्वन् ! (राजन्) विद्या और विनय से प्रकाशमान (ते) आपके समीप जो (वसुता) द्रव्यों का होना उसमें वर्त्तमान (पुरूणि) बहुत और (पुरुधा) बहुत प्रकारों से धारण किये हुए (वसूनि) द्रव्यों को (त्वाया) आपके साथ मैं (अश्याम्) प्राप्त होऊँ और हे (पुरुवार) बहुतों से स्वीकार करने योग्य (अग्ने) विद्या और विनय से प्रकाशमान (हि) निश्चय से (त्वे) आप में (पुरूणि) बहुत द्रव्य (सन्ति) हैं (राजनि) राजा (त्वे) आपके होने पर (वसु) द्रव्य का (विधते) विधान करनेवाले के लिये कल्याण होता है, वह आप हमारे राजा हूजिये ॥१३॥
सनेम तेऽवसा नव्य इन्द्र प्र पूरवः स्तवन्त एना यज्ञैः।
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दर्द्धन्दासीः पुरुकुत्साय शिक्षन् ॥१०॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 20; मन्त्र » 10)
हे (इन्द्र) अत्यन्त ऐश्वर्य और सुख के देनेवाले ! (ते) आपके (अवसा) रक्षण आदि से हम लोग (सप्त) सात (पुरः) नगरियों का (सनेम) विभाग करें और जैसे (पूरवः) मनुष्य (एना) इस (अवसा) रक्षण आदि से और (यज्ञैः) श्रेष्ठ व्यवहाररूप यज्ञों से (स्तवन्ते) स्तुति करते हैं इससे (नव्यः) नवीनों में हुए आप उनसे स्तुति करिये और (यत्) जो (शर्म) गृह और (शारदीः) शरत्काल में हुई (दासीः) सेविकाओं को प्राप्त होके (पुरुकुत्साय) बहुत शस्त्रवाले के लिये (शिक्षन्) शिक्षा देता हुआ दुःखों को (प्र, दर्त्) नष्ट करता है और शत्रुओं को (हन्) मारता है, वह सब से सत्कार करने योग्य है ॥१०॥
दस्यु की तरह, शब्द ‘दास’ का इस्तेमाल भी उन स्वदेशी लोगों के लिए किया जाता था जो आक्रमणकारियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि दास और दस्यु से तात्पर्य दुष्टआत्माएँ हैं, लेकिन इस विचार के पक्ष में कोई तर्क नहीं है। ग्रिफिथ लिखते हैं:
“यह शब्द मूल रूप से उन विशेष दुष्टआत्माओं के लिए गढ़ा गया था, जिन्हें इंद्र और मनुष्यों का शत्रु माना जाता था, लेकिन आम तौर पर इसका अर्थ उन बर्बर लोगों से है जो देश के मूल निवासी थे, और जिनके साथ मूल रूप से आर्य प्रवासी की लड़ाई थी।”
एक अन्य स्थान पर, वही लेखक इस की व्याख्या करते हुए लिखता है कि:
यह उन बर्बर कुरूप निवासियों को संदर्भित करता है जिन्हें आर्य प्रवासियों द्वारा भूतों और पिशाचों के वर्ग में शामिल कर दिया गया था।”
दास और वस्यु की पहचान निर्धारित करने में उस समय संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, जब हम ऋग्वेद में ही उनके मानव होने के अंतर्पाठीय प्रमाण देखते हैं। जहाँ उन्हें जगह-जगह अधर्मी कहा गया है। उन्हें अज्ञात क़ानूनों का पालन करनेवाला और बुद्धिविहीन ठहराया गया है। उनके पास गायों, बैलों और मवेशियों की बहुतायत है, उनके पास क़िले हैं जिन्हें आर्य जीतते हैं। इन सबसे मज़बूत प्रमाण यह है कि उनकी नाक चिपटी, उनके जबड़े चौड़े और उनका रंग काला बताया गया है, जो आज भी हम प्राचीन द्रविड़ जाति के लोगों में देखते हैं।
द्यौर्न य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शवसा पृत्सु जनान्।
तं नः सहस्रभरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम् ॥१॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 20; मन्त्र » 1)
हे (सहसः) बल से (सूनो) श्रेष्ठ पुत्र (इन्द्र) अत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त ! (यः) जो (द्यौः) बिजुली वा सूर्य के (न) समान प्रकाशित (रयिः) धन है इस का (अर्यः) स्वामी (शवसा) बल से (पृत्सु) सङ्ग्रामों में (जनान्) मनुष्यों के प्रति (अभि) सम्मुख (तस्थौ) वर्त्तमान होवे (तम्) उस (सहस्रभरम्) असंख्य को धारण करनेवाले (वृत्रतुरम्) जैसे मेघों को, वैसे शत्रुओं को नाश करता है जिससे उस तथा (उर्वरासाम्) बहुत श्रेष्ठ भूमियों में श्रेष्ठ विजय को (नः) हम लोगों के लिये (दद्धि) दीजिये जिससे हम लोग लक्ष्मीवान् (भूम) होवें ॥१॥
अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरंहूरणाभूत्।
बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इन्द्र पन्थाम् ॥२०॥
दिवेदिवे सदृशीरन्यमर्धं कृष्णा असेधदप सद्मनो जाः।
अहन्दासा वृषभो वस्नयन्तोदव्रजे वर्चिनं शम्बरं च ॥२१॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 47; मन्त्र » 20,21)
हे (बृहस्पते) बड़ों के पालन करने (चिकित्सा) रोगों की परीक्षा करने और (इन्द्र) रोग और दोषों के दूर करनेवाले वैद्यराज ! आपके सहाय से (उर्वी) बहुत फल आदि से युक्त (सती) वर्त्तमान (अंहूरणा) चलनेवालों का सङ्ग्राम जिसमें वह (भूमिः) पृथिवी (अभूत्) होती है और जहाँ (अगव्यूति) दो कोश के परिमाण से रहित (क्षेत्रम्) निवास करते हैं जिस स्थान में ऐसा स्थान होता है उसको (देवाः) विद्वान् हम लोग (आ, अगन्म) सब प्रकार से प्राप्त होवें (इत्था) इस प्रकार से वा इस हेतु से (गविष्टौ) उत्तम प्रकार शिक्षितवाणी की सङ्गति में (सते) वर्त्तमान (जरित्रे) स्तुति करनेवाले के लिये (पन्थाम्) मार्ग को (प्र) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें ॥२०॥ हे मनुष्यो ! जैसे (जाः) प्रकट हुआ सूर्य्य (दिवेदिवे) प्रतिदिन (सदृशीः) तुल्यस्वरूपयुक्त (कृष्णाः) ख़राब वर्णवाली वा खोदी गई पृथिवियों और (अन्यम्) अन्य (अर्द्धम्) आधे को (च) भी (असेधत्) अलग करता है और (सद्मनः) निवास करते हैं जिसमें उस गृह के अन्धकार को (अप) अलग करता है तथा (वृषभः) वृष्टि करनेवाला (उदव्रजे) जल जाते हैं जिसमें उसमें (वर्चिनम्) प्रकाशमान (शम्बरम्) मेघ का (अहन्) नाश करता है, वैसे (वस्नयन्ता) निवास करते हुए के समान आचरण करते हुए राजा और प्रजाजन (दासा) उपेक्षा करनेवाले हुए वर्त्ताव करें ॥२१॥
जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थे।
अनाविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु ॥१॥
धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम।
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥२॥
वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं परिषस्वजाना।
योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥३॥
ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे।
अप शत्रून्विध्यतां संविदाने आर्त्नी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान् ॥४॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 6; सूक्त » 75; मन्त्र » 1-4)
हे वीर ! (यत्) जो (जीमूतस्येव) मेघ के समान (प्रतीकम्) प्रतीति करनेवाला वर्म (भवति) होता है, उससे (वर्मी) कवचधारी होकर (समदाम्) अहङ्कारों के साथ वर्त्तमान सङ्ग्रामों के (उपस्थे) समीप (याति) जाता है तथा (अनाविद्धया) शस्त्रास्त्ररहित अर्थात् अनविधे (तन्वा) शरीर से (त्वम्) तुम शत्रुओं को (जय) जीतो (सः) सो (वर्मणः) कवच का (महिमा) महत्त्व (त्वा) तुम्हें (पिपर्तु) पाले ॥१॥ हे वीर पुरुषो ! जो (धनुः) धनुष् (शत्रोः) शत्रु के (अपकामम्) काम का विनाश (कृणोति) करात है जिस (धन्वना) धनुष् से जैसे हम (गाः) भूमियों को (धन्वना) धनुष् से (आजिम्) सङ्ग्राम को (जयेम) जीतें (धन्वना) धनुष् से (तीव्राः) कठिन तेज (समदः) सङ्ग्रामों को (जयेम) जीतें और (धन्वना) धनुष् से (सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशा प्रदिशाओं में स्थित जो शत्रुजन उनको (जयेम) जीतें, वैसे उससे तुम भी उनको जीतो ॥२॥ हे शूरवीर ! जो (इयम्) यह (ज्या) प्रत्यञ्चा अर्थात् धनुष् की तांति (वक्ष्यन्तीव) जैसे विदुषी कहनेवाली होती, वैसे (प्रियम्) अपने प्यारे (सखायम्) मित्र के समान वर्त्तमान पति को (परिषस्वजाना) सब ओर से संग किये हुए (योषेव) पत्नी स्त्री (कर्णम्) कान को (आ, गनीगन्ति) निरन्तर प्राप्त होती है, वैसे (अधि) (धन्वन्) धनुष् के ऊपर (वितता) विस्तारी हुई तांति (समने) सङ्ग्राम में (पारयन्ती) पार को पहुँचाती हुई (शिङ्क्ते) गूँजती है उस (इत्) ही को तुम यथावत् जानकर उसका प्रयोग करो ॥३॥ हे वीरपुरुषो ! (ते) वे दोनों (इमे) ये (संविदाने) प्रतिज्ञा पालनेवालियों के समान वा (अमित्रान्) शत्रुजनों को (विष्फुरन्ती) कंपाती (आर्त्नी) वेग से जाती और (आचरन्ती) सब ओर से प्रिय आचरण करती हुई (योषा) पत्नी स्त्री जैसे (समनेव) समान मनवाली, वैसे वा (पुत्रम्) पुत्र को जैसे (मातेव) माता, वैसे (उपस्थे) समीप में विजय को (बिभृताम्) धारण करें और (शत्रून्) शत्रुजनों को (अप, विध्यताम्) पीटें ॥४॥
नि दुर्ग इन्द्र श्नथिह्यमित्रानभि ये नो मर्तासो अमन्ति।
आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा नो भर संभरणं वसूनाम् ॥२॥
शतं ते शिप्रिन्नूतयः सुदासे सहस्रं शंसा उत रातिरस्तु।
जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे द्युम्नमधि रत्नं च धेहि ॥३॥
कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहो देवजूतमियानाः
। सत्रा कृधि सुहना शूर वृत्रा वयं तरुत्राः सनुयाम वाजम् ॥५॥
एवा न इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र ते महीं सुमतिं वेविदाम।
इषं पिन्व मघवद्भ्यः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 7; सूक्त » 25; मन्त्र » 2-3,5-6)
हे (इन्द्र) दुष्ट शत्रुओं के निवारनेवाला राजा ! (ये) जो (मर्त्तासः) मनुष्य (नः) हम लोगों को (दुर्गे) शत्रुओं को दुःख से पहुँचने योग्य परकोटा में (अमन्ति) रोगों को पहुँचाते हैं उन (अमित्रान्) सब के साथ द्रोहयुक्त रहने वालों को आप (नि, अभि, श्नथिहि) निरन्तर सब ओर से मारो, हम लोगों से (आरे) दूर उनको फेंको (निनित्सोः) और निन्दा की इच्छा करनेवाले से हम लोगों को दूर कर (नः) हम लोगों के (तम्) उस (शंसम्) प्रशंसनीय विजय को (कृणुहि) कीजिये तथा (वसूनाम्) द्रव्यादि पदार्थों के (संभरणम्) अच्छे प्रकार पोषण को (आ, भर) सब ओर से स्थापित कीजिये ॥२॥ हे (शिप्रिन्) अच्छे मुखवाले राजा ! (ते) आपके (वनुषः) याचना करते हुए पीड़ित मनुष्य की (शतम्) सैकड़ों (ऊतयः) रक्षा आदि क्रिया और (सहस्रम्) असंख्य (शंसाः) प्रशंसा हों (उत) और (सुदासे) जो उत्तमता से देता है उसके लिये (रातिः) दान (अस्तु) हो आप (वनुषः) अधर्म से माँगनेवाले पाखण्डी (मर्त्यस्य) मनुष्य की (वधः) ताड़ना को (जहि) हनो, नष्ट करो तथा (अस्मे) हम लोगों में (द्युम्नम्) धर्मयुक्त यश और (रत्नं च) रमणीय धन भी (अधि, धेहि) अधिकता से धारण करो ॥३॥
हे (शूर) निर्भय ! जिन (इन्द्रे) परमैश्वर्य्ययुक्त आप में (हर्यश्वाय) प्रशंसित जिसके मनुष्य वा घोड़े उसके लिये (एते) ये (कुत्साः) वज्र अस्त्र और शस्त्र आदि समूह हों उनको और (देवजूतम्) देवों से पाये हुए (शूषम्) बल तथा (सहः) क्षमा (इयानाः) प्राप्त होते हुए (तरुत्राः) दुःख से सबको अच्छे प्रकार तारनेवाले (वयम्) हम लोग (वाजम्) विज्ञान को (सनुयाम) याचें आप (सत्रा) सत्य से (वृत्रा) दुःखों को (सुहना) नष्ट करने के लिये सुगम (कृधि) करो ॥ ५ ॥ हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देनेवाले ! आप (नः) हम लोगों को विद्या और उत्तम शिक्षा से (प्र, पूर्धि) अच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग (वार्यस्य) स्वीकार करने योग्य (ते) आपकी (सुमतिम्) उत्तम मति और (महीम्) अत्यन्त वाणी को (वेविदाम) प्राप्त हों तथा (मघवद्भ्यः) बहुत धन से युक्त सज्जनों से (सुवीराम्) उत्तम विज्ञानवान् वीर जिसमें होते उस (इषम्) विद्या को प्राप्त होवें, यहाँ आप हम लोगों की (पिन्व) रक्षा करो और (यूयम्) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा, एव) सर्वदैव (पात) रक्षा करो ॥६॥
परा णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि।
अस्माकं बोध्यविता महाधने भवा वृधः सखीनाम् ॥२५॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 7; सूक्त » 32; मन्त्र » 25)
हे (मघवन्) बहुधनयुक्त राजा (सुवेदाः) धर्म से उत्पन्न किये हुए ऐश्वर्ययुक्त ! आप (नः) हमारे (अमित्रान्) शत्रुओं को (परा, णुदस्व) प्रेरो हमारे लिये (वसु) धन को (कृधि) सिद्ध करो (महाधने) बड़े वा बहुत धन जिसमें प्राप्त होते हैं उस संग्राम में (अस्माकम्) हमारे (सखीनाम्) सर्व मित्रों के (अविता) रक्षा करनेवाले (बोधि) जानिये और (वृधः) बढ़नेवाले (भव) हूजिये ॥२५॥
त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । संस्थे जनस्य गोमतः ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 21; मन्त्र » 11)
(वृषभ) हे शस्त्रों की वर्षा करनेवाले! (वयम्) हम सब प्रजाजन (गोमतः, जनस्य, संस्थे) तेजस्वी समुदाय के युद्ध में (त्वया, युजा, ह, स्वित्) आपकी सहायता ही से (श्वसन्तम्) क्रोध से उच्च श्वास लेते हुए शत्रु का (प्रतिब्रुवीमहि) प्रतिवचन=तिरस्कार करते हैं ॥११॥
अपि वृश्च पुराणवद्व्रततेरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय ।
वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 40; मन्त्र » 6)
हे शक्तिशाली शासक! (व्रततेः) बेल के (गुष्पितम्) उलझे गुच्छे को (पुराणवत्) जैसे कि पुराना हो तो सरलता से (वृश्च) काट देते हैं वैसे ही (दासस्य) क्षीण करने वाले विध्वंसक दुष्ट जन के (गुष्पितम्) पुंजीभूत (ओजः) तेज को काट (अपि) और उसे (दम्भय) अपने आदेश के अआधीन कर ले। (वयम्) हम प्रजाजन (अस्य) इसके (तत्) उस (इन्द्रेण) बलशाली राजा इत्यादि द्वारा (सम्भृतम्) एकत्र किए हुए वसुतेजरूपी ऐश्वर्य का (विभजेमहि) बाँटकर सेवन करें॥६॥
अयं ते मानुषे जने सोम: पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥
अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधि प्रियः । आर्जीकीये मदिन्तमः ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 64; मन्त्र » 10,11)
हे इन्द्र ! (ते) तेरे लिये (मानुषे+जने) मुझ मनुष्य के निकट और (पूरुषु) सम्पूर्ण मनुष्यजातियों में (अयम्+सोमः+सूयते) यह तेरा प्रिय सोमयाग किया जाता है, (तस्य+एहि) उसके निकट आ, (प्रद्रव) उसके ऊपर कृपा कर, (पिब) कृपादृष्टि से उसको देख ॥१० ॥ हे इन्द्र! (शर्य्यणावति) इस विनश्वर शरीर में (सुसोमायाम्) इस रसमयी बुद्धि में और (आर्जीकीये) समस्त इन्द्रियों के सहयोग में (अधिश्रितः) आश्रित (ते) तेरे अनुग्रह से (मदिन्तमः) तेरा आनन्दजनक याग सदा हो रहा है । इसको ग्रहण कीजिये ॥११ ॥
जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम् ।
विद्मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दा: ॥
सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तमुरुं गभीरं पृथुबुध्नमिन्द्र ।
श्रुतऋषिमुग्रमभिमातिषाहमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दा: ॥
सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम् ।
दस्युहनं पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दा: ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 10; सूक्त » 47; मन्त्र » 1,3,4)
(वसूनां वसुपते शूर इन्द्र) हे धनों के धनस्वामिन् व्यापक परमात्मन्! (वसूयवः) हम धन की कामना करनेवाले (ते दक्षिणं हस्तं जगृभ्म) तेरे देनेवाले हस्तरूप साधन को पकड़ते हैं-हाथ के समान आश्रय को ग्रहण करते हैं (त्वा गोनां गोपतिं विद्म हि) तुझ सुख प्राप्त करानेवाले पदार्थों के स्वामी को हम जानते हैं-मानते हैं-उपासना में लाते हैं (अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः) हमारे लिए दर्शनीय अपने स्वरूप को और सुखवर्षक आत्मपोषक धन को दे ॥१॥ (सुब्रह्माणम्) शोभन वेदज्ञान के स्वामी (देवयन्तम्) मुमुक्षुओं के चाहनेवाले (बृहन्तम्) सर्वतो महान् (उरुम्) अनन्त (गभीरम्) अपार (पृथुबुध्नम्) सब जगत् के प्रथितमूल (श्रुतऋषिम्) ऋषियों द्वारा श्रवण करने योग्य (उग्रम्) सब के ऊपर विराजमान (अभिमातिषहम्) अभिमानी जनों के दबानेवाले परमात्मा को जानते हैं-मानते हैं (इन्द्र) वह तू इन्द्र ! (अस्मभ्यम्…) पूर्ववत् ॥३॥ (सनद्वाजम्) अमृतान्न के सम्भाजक (विप्रवीरम्) मेधावी उपासकोंवाले (तरुतारम्) संसारसागर तरानेवाले, (धनस्पृतम्) धनप्राप्त करानेवाले (शूशुवांसम्) बढ़ानेवाले या व्यापनेवाले (सुदक्षम्) श्रेष्ठ बलवाले (दस्युहनम्) दुष्टनाशक (पूर्भिदम्) पापपुरों-मन की वासना के नाशक (सत्यम्) अविनाशी तुझ परमात्मा को हम जानते हैं-मानते हैं (अस्मभ्यम्) पूर्ववत् ॥४॥
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम् ॥
नृचक्षा रक्ष: परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा ।
तस्याग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 10; सूक्त » 87; मन्त्र » 5,10)
(जातवेदः-अग्ने) हे प्राप्त अवसर को जाननेवाले अग्रणी सेनानायक! तू (यातुधानस्य-त्वचं भिन्धि) यातना देनेवाले की त्वचा को उखेड़ दे (हिंस्रा-अशनिः-हरसा-एनं हन्तु) नाशकारिणी विद्युत् अपने तेज से उनको मारे (पर्वाणि प्र शृणीहि) जोड़ों-अङ्गों को तोड़ दे (वृक्णं क्रविष्णुः क्रव्यात्-विचिनोतु) कटे हुए शरीर को मांस इच्छुक मांसभक्षक पशु-पक्षी नोच-नोच कर खावें ॥५॥ (अग्ने) हे अग्रणायक सेनानी ! (नृचक्षाः) तू राष्ट्रनायकों का द्रष्टा हुआ (विक्षु रक्षः परि पश्य) प्रजाजनों में राक्षस-दुष्टजन को टटोल (तस्य त्रीणि-अग्रा-प्रति शृणीहि) उसके तीन मुख्यों सेनाबलों को नष्ट कर (तस्य पृष्टीः) उसके पार्श्वभागों-पक्ष लेनेवालों को नष्ट कर (यातुधानस्य मूलं वृश्च) पीड़ा देनेवाले के वेश या शस्त्रागार या छावनी को नष्ट कर ॥१०॥
अभिख्या नो मघवन्नाधमानान्त्सखे बोधि वसुपते सखीनाम् ।
रणं कृधि रणकृत्सत्यशुष्माभक्ते चिदा भजा राये अस्मान् ॥
(ऋग्वेद - मण्डल » 10; सूक्त » 112; मन्त्र » 10)
(वसुपते) हे वसुपालक तुझमें बसनेवालों के पालक (मघवन्) ऐश्वर्यवाले (सखे) हे मित्र परमात्मन्! (नः नाधमानान्) हम याचना करते हुओं को (अभिख्या) आभिमुख्यरूप से देख (सखीनां बोधि) हमें अपने मित्रों को बोध दे या हमें जान (रणकृत्) हमारे विरोधी कामादियों से युद्ध करनेवाले! (रणम्-कृधि) तू युद्ध कर (सत्यशुष्म) हे सत्यबलवाले-नित्य बलवन्! (अभक्ते चित्) जो धन तूने किसी के लिये भक्त नहीं किया-नहीं दिया, उस अपने आनन्दरसरूप धन में (राये) ऐश्वर्य में (अस्मान्) हमें (आ भज) भलीभाँति भागी बना ॥१०॥
देवा: कपोत इषितो यदिच्छन्दूतो निॠत्या इदमाजगाम । तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥
ऋग्वेद - मण्डल » 10; सूक्त » 165; मन्त्र » 1
(देवाः) हे संग्राम जीतने के इच्छुक विद्वानों! (इषितः) दूसरों से प्रेरित हुआ भेजा हुआ (कपोतः-दूतः) भाषा वेश की दृष्टि से विविध रंगवाला विचित्रभाषी सन्देशवाहक अथवा हमारे द्वारा भेजा हुआ दूत (यत्-इच्छन्) जिस वृत्त को सूचित करने की इच्छा रखता हुआ (निर्ऋत्याः) परभूमि से-सीमा से तथा अपनी भूमि से (इदम्-आ जगाम) इस स्थान को प्राप्त हुआ है (तस्मै-अर्चाम) उसके लिए सत्कार करते हैं (निष्कृतिं-कृणवाम) उसका प्रतिकार या समाधान करें (नः) हमारे (द्विपदे शम्) दो पैरवाले मनुष्यादि के लिये कल्याण हो (चतुष्पदे-शम्-अस्तु) हमारे चार पैरवाले पशु के लिए कल्याण हो ॥१॥
(स्वामी दयानन्द सरस्वती के संस्कृत भाष्य के आधार पर)
यजुर्वेद
बजरुवेद में हमें युद्ध से संबंधित निम्नलिखित मंत्र मिलते हैं:
वि न ऽइन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । यो अस्माँ अभिदासत्यधरङ्गमया तमः । उपयामगृहीतो सीन्द्राय त्वा विमृधे ऽएष ते योनिरिन्द्राय त्वा विमृधे ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 8; मन्त्र » 44)
हे (इन्द्र) सेनापते! तू (नः) हमारे (पृतन्यतः) हम से युद्ध करने के लिये सेना की इच्छा करनेहारे शत्रुओं को (जहि) मार और उन (नीचा) नीचों को (यच्छ) वश में ला और जो शत्रुजन (अस्मान्) हम लोगों को (अभिदासति) सब प्रकार दुःख देवे उस (विमृधः) दुष्ट को (तमः) जैसे अन्धकार को सूर्य्य नष्ट करता है, वैसे (अधरम्) अधोगति को (गमय) प्राप्त करा, जिस (ते) तेरा (एषः) उक्त कर्म्म करना (योनिः) राज्य का कारण है, इससे तू हम लोगों से (उपयामगृहीतः) सेना आदि सामग्री से ग्रहण किया हुआ (असि) है, इसी से (त्वा) तुझ को (विमृधे) जिस में बड़े-बड़े युद्ध करने वाले शत्रुजन हैं, (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य देने वाले उस युद्ध के लिये स्वीकार करते हैं (त्वा) तुझ को (विमृधे) जिस के शत्रु नष्ट हो गये हैं, उस (इन्द्राय) राज्य के लिये प्रेरणा देते हैं अर्थात् अधर्म्म से अपना वर्त्ताव न वर्त्ते॥४४॥
अग्ने सहस्व पृतनाऽअभिमातीरपास्य ।
दुस्टरस्तरन्नरातीर्वर्चाधा यज्ञवाहसि ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 9; मन्त्र » 37)
हे (अग्ने) सब विद्या जानने वाले विद्वान् राजन्! (दुष्टरः) दुःख से तरने योग्य (तरन्) शत्रु सेना को अच्छे प्रकार तरते हुए आप (यज्ञवाहसि) जिसमें राजधर्मयुक्त राज्य में (अभिमातीः) अभिमान आनन्दयुक्त (पृतनाः) बल और अच्छी शिक्षायुक्त वीरसेना को (सहस्व) सहो (अरातीः) दुःख देने वाले शत्रुओं को (अपास्य) दूर निकालिये और (वर्चः) विद्या बल और न्याय को (धाः) धारण कीजिये॥३७॥
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम् ।
धनञ्जयँ रणेरणे ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 11; मन्त्र » 34)
हे वीर पुरुष! जो आप (पाथ्यः) अन्न जल आदि पदार्थों की सिद्धि में कुशल (वृषा) पराक्रमी (रणेरणे) प्रत्येक युद्ध में शूरता आदि युक्त विद्वान् हैं (तम्) पूर्वोक्त पदार्थविद्या जानने (धनञ्जयम्) शत्रुओं से धन जीतने (उ) और (दस्युहन्तमम्) अतिशय करके डाकुओं को मारने वाले (त्वा) आप को वीरों की सेना राजधर्म्म की शिक्षा से (समीधे) प्रदीप्त करे॥३४॥
योऽअस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो द्वेषते जनः ।
निन्दाद्योऽअस्मान्धिप्साच्च सर्वन्तम्भस्मसा कुरु ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 11; मन्त्र » 80)
हे सभा और सेना के स्वामिन्! आप (यः) जो (जनः) मनुष्य (अस्मभ्यम्) हम धर्मात्माओं के लिये (अरातीयात्) शत्रुता करे (यः) जो (नः) हमारे साथ (द्वेषते) दुष्टता करे (च) और हमारी (निन्दात्) निन्दा करे (यः) जो (अस्मान्) हम को (धिप्सात्) दम्भ दिखावे (च) और हमारे साथ छल करे (तम्) उस (सर्वम्) सब को (भस्मसा) जला के सम्पूर्ण भस्म (कुरु) कीजिये॥८०॥
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँऽ ओषतात्तिग्महेते ।
यो नो अरातिँ समिधान चक्रे नीचा तन्धक्ष्यतसन्न शुष्कम् ॥
ऊर्ध्वा भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने ।
अव स्थिरा तनुहि यातुजूनाञ्जामिमजामिम्प्र मृणीहि शत्रून् ।
अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 13; मन्त्र » 12-13)
हे (अग्ने) तेजधारी सभा के स्वामी! आप राजधर्म के बीच (उत्तिष्ठ) उन्नति को प्राप्त हूजिये। धर्मात्मा पुरुषों के (प्रति) लिये (आतनुष्व) सुखों का विस्तार कीजिये। हे (तिग्महेते) तीव्र दण्ड देने वाले राजपुरुष! (अमित्रान्) धर्म के द्वेषी शत्रुओं को (न्योषतात्) निरन्तर जलाइये। हे (समिधान) सम्यक् तेजधारी जन! (यः) जो (नः) हमारे (अरातिम्) शत्रु को उत्साही (चक्रे) करता है, (तम्) उसको (नीचा) नीची दशा में करके (शुष्कम्) सूखे (अतसम्) काष्ठ के (न) समान (धक्षि) जलाइये॥१२॥ हे (अग्ने) तेजस्विन् विद्वान् पुरुष! जिसलिये आप (ऊर्ध्वः) उत्तम (भव) हूजिये, धर्म के (प्रति) अनुकूल होके (विध्य) दुष्ट शत्रुओं को ताड़ना दीजिये, (अस्मत्) हमारे (स्थिरा) निश्चल (दैव्यानि) विद्वानों के रचे पदार्थों को (आविः) प्रकट (कृणुष्व) कीजिये, सुखों को (तनुहि) विस्तारिये, (यातुजूनाम्) परपदार्थों को प्राप्त होने और वेग वाले शत्रुजनों के (जामिम्) भोजन के और (अजामिम्) अन्य व्यवहार के स्थान को (अव) अच्छे प्रकार विस्तारपूर्वक नष्ट कीजिये और (शत्रून्) शत्रुओं को (प्रमृणीहि) बल के साथ मारिये, इसिलिये मैं (त्वा) आपको (अग्नेः) अग्नि के (तेजसा) प्रकाश के (अधि) सम्मुख (सादयामि) स्थापन करता हूं॥१३॥
अयम्पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रथगृत्सश्च रथौजाश्च सेनानीग्रामण्या ।
पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ दङ्क्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुषेयो वधः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषाञ्जम्भे दध्मः ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 15; मन्त्र » 15)
जो (अयम्) यह (पुरः) पूर्वकाल में वर्त्तमान (हरिकेशः) हरितवर्ण केश के समान हरणशील और क्लेशकारी ताप से युक्त (सूर्यरश्मिः) सूर्य की किरणें हैं, (तस्य) उनका (रथगृत्सः) बुद्धिमान् सारथि (च) और (रथौजाः) रथ के ले चलने के वाहन (च) इन दोनों के तथा (सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति और ग्राम के अध्यक्ष के समान अन्य प्रकार के भी किरण होते हैं, उन किरणों की (पुञ्जिकस्थला) सामान्य प्रधान दिशा (च) और (क्रतुस्थला) प्रज्ञाकर्म को जतानेवाली उपदिशा (च) ये दोनों (अप्सरसौ) प्राणों में चलने वाली अप्सरा कहाती हैं, जो (दङ्क्ष्णवः) मांस और घास आदि पदार्थों को खाने वाले व्याघ्र आदि (पशवः) हानिकारक पशु हैं, उनके ऊपर (हेतिः) बिजुली गिरे। जो (पौरुषेयः) पुरुषों के समूह (वधः) मारनेवाले और (प्रहेतिः) उत्तम वज्र के तुल्य नाश करने वाले हैं, (तेभ्यः) उन के लिये (नमः) वज्र का प्रहार (अस्तु) हो और जो धार्मिक राजा आदि सभ्य राजपुरुष हैं, (ते) वे उन पशुओं से (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (नः) हम को (मृडयन्तु) सुखी करें, (ते) वे रक्षक हम लोग (यम्) जिस हिंसक से (द्विष्मः) विरोध करें (च) और (यः) जो हिंसक (नः) हम से (द्वेष्टि) विरोध करे (तम्) उसको हम लोग (एषाम्) इन व्याघ्रादि पशुओं के (जम्भे) मुख में (दध्मः) स्थापन करें॥१५॥
बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमानऽउग्रः
। अभिवीरोऽअभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित् ॥
गोत्रभिदङ्गोविदँवज्रबाहुञ्जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ।
इमँ सज़ाताऽअनु वीरयध्वमिन्द्रँ सखायो अनु सँ रभध्वम् ॥
अमीषाञ्चित्तम्प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि ।
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥
(यजुर्वेद - अध्याय » 17; मन्त्र » 37, 38, 44)
हे (इन्द्र) युद्ध की उत्तम सामग्री युक्त सेनापति! (बलविज्ञायः) जो अपनी सेना को बली करना जानता (स्थविरः) वृद्ध (प्रवीरः) उत्तम वीर (सहस्वान्) अत्यन्त बलवान् (वाजी) जिसको प्रशंसित शास्त्रबोध है, (सहमानः) जो सुख और दुःख को सहने तथा (उग्रः) दुष्टों के मारने में तीव्र तेज वाला (अभिवीरः) जिस के अभीष्ट अर्थात् तत्काल चाहे हुए काम के करने वाले वा (अभिसत्वा) सब ओर से युद्धविद्या में कुशल रक्षा करनेहारे वीर हैं, (सहोजाः) बल से प्रसिद्ध (गोवित्) वाणी, गौओं वा पृथिवी को प्राप्त होता हुआ, ऐसा तू युद्ध के लिये (जैत्रम्) जीतने वाले वीरों से घेरे हुए (रथम्) पृथिवी, समुद्र और आकाश में चलने वाले रथ को (आ, तिष्ठ) आकर स्थित हो अर्थात् उसमें बैठ॥३७॥ हे (सज़ाताः) एकदेश में उत्पन्न (सखायः) परस्पर सहाय करने वाले मित्रो! तुम लोग (ओजसा) अपने शरीर और बुद्धि वा बल वा सेनाजनों से (गोत्रभिदम्) जो कि शत्रुओं के गोत्रों अर्थात् समुदायों को छिन्न-भिन्न करता, उनकी जड़ काटता (गोविदम्) शत्रुओं की भूमि को ले लेता (वज्रबाहुम्) अपनी भुजाओं में शस्त्रों को रखता (प्रमृणन्तम्) अच्छे प्रकार शत्रुओं को मारता (अज्म) जिससे वा जिसमें शत्रुजनों को पटकते हैं, उस संग्राम में (जयन्तम्) वैरियों को जीत लेता और (इमम्) उनको (इन्द्रम्) विदीर्ण करता है, इस सेनापति को (अनु, वीरयध्वम्) प्रोत्साहित करो और (अनु, संरभध्वम्) अच्छे प्रकार युद्ध का आरम्भ करो॥३८॥
हे (अप्वे) शत्रुओं के प्राणों को दूर करनेहारी राणी क्षत्रिया वीर स्त्री! (अमीषाम्) उन सेनाओं के (चित्तम्) चित्त को (प्रतिलोभयन्ती) प्रत्यक्ष में लुभाने वाली जो अपनी सेना है, उसके (अङ्गानि) अङ्गों को तू (गृहाण) ग्रहण कर अधर्म्म से (परेहि) दूर हो, अपनी सेना को (अभि, प्रेहि) अपना अभिप्राय दिखा और शत्रुओं को (निर्दह) निरन्तर जला, जिससे ये (अमित्राः) शत्रुजन (हृत्सु) अपने हृदयों में (शोकैः) शोकों से (अन्धेन) आच्छादित हुए (तमसा) रात्रि के अन्धकार के साथ (सचन्ताम्) संयुक्त रहें॥४४॥
हिन्दी अनुवादः स्वामी दयानन्द सरस्वती
(स्वामी दयानन्द सरस्वती के संस्कृत भाष्य के आधार पर)
मंत्र 44 में एक शब्द है (अप्वे) वैदिक देवमाला में महामारी की देवी का नाम “अपवा” है। यहाँ संभवत: इसका आशय उन बीमारियों से है जो युद्ध के दौरान सेनाओं में फैलती हैं (यजुर्वेद ग्रिफिथ का अनुवाद पृष्ठ 154)।
सामवेद
सामवेद के जिन मंत्रों में युद्ध का विषय आता है वे हैं:
नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमैरमित्रमर्दय ॥११॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 11)
हे (देव) ज्योतिर्मय तथा विद्या आदि ज्योति के देनेवाले (अग्ने) लोकनायक जगदीश्वर अथवा राजन्! (कृष्टयः) मनुष्य (ते) आपके (ओजसे) बल के लिए (नमः) नमस्कार के वचन (गृणन्ति) उच्चारण करते हैं, अर्थात् बार-बार आपके बल की प्रशंसा करते हैं। आप (अमैः) अपने बलों से (अमित्रम्) शत्रु को (अर्दय) नष्ट कर दीजिए ॥१॥
अग्ने रक्षा णो अꣳहसः प्रति स्म देव रीषतः । तपिष्ठैरजरो दह ॥२४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 24)
हे (अग्ने) ज्योतिष्मन् परमात्मन् ! आप (नः) हमारा (अंहसः) पापाचरण से (रक्ष त्राण) कीजिए। हे (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभाव, सकलैश्वर्यप्रदाता, प्रकाशमान, सर्वप्रकाशक जगदीश्वर! (अजरः)
स्वयं नश्वरता, जर्जरता आदि से रहित आप (रिषतः) हिंसापरायण आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं को (तपिष्ठैः) अतिशय संतापक स्वकीय सामर्थ्यों से (प्रति दह स्म) भस्मसात् कर दीजिए ॥४॥
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये ।
अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतूर्तिमनेहसम् ॥६२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 62)
(मर्तासः) मरणधर्मा, (सखायः) समान ख्यातिवाले हम साथी लोग (देवम्) ज्योतिर्मय और ज्योति देनेवाले, (अपां नपातम्) व्याप्त प्रकृति का और जीवात्माओं का विनाश न करनेवाले, (सुभगम्) उत्तम ऐश्वर्यवाले, (सुदंससम्) शुभ कर्मोंवाले, (सुप्रतूर्तिम्) अत्यन्त शीघ्रता से कार्यों को करनेवाले, (अनेहसम्) हिंसा न किये जा सकने योग्य, निष्पाप, सज्जनों के प्रति क्रोध न करनेवाले (त्वा) तुझ परमेश्वररूप अग्नि को (ऊतये) आत्मरक्षा और प्रगति के लिए (ववृमहे) वरण करते हैं ॥८॥
प्रत्यग्ने हरसा हरः शृणाहि विश्वतस्परि ।
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्यम् ॥९५॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 95)
हे (अग्ने) ज्योतिर्मय परमेश्वर, मेरे अन्तरात्मा, राजा, सेनापति और आचार्यप्रवर ! आप (यातुधानस्य) यातना देनेवाले (रक्षसः) पापरूप राक्षस के तथा पापी दुष्ट शत्रु के (बलम्) सैन्य को, और (वीर्यम्) पराक्रम को (न्युब्ज) निर्मूल कर दीजिए। (विश्वतः परि) सब ओर से (तस्य) उसके (हरः) हरणसामर्थ्य, क्रोध और तेज को (हरसा) अपने हरणसामर्थ्य, मन्यु और तेज से (प्रतिशृणाहि) विनष्ट कर दीजिए ॥५॥
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । वसु स्पार्हं तदा भर ॥१३४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 134)
हे इन्द्र! विद्यावीर, दयावीर, बलवीर परमात्मन् राजन् व आचार्य ! आप (विश्वाः) सब (द्विषः) द्वेष-वृत्तियों को और काम, क्रोध, लोभ आदि असुरों तथा मानव राक्षसों की सेनाओं को (अप भिन्धि) विदीर्ण कर दीजिए। (बाधः) बाधक, सन्मार्ग में विघ्न डालनेवाले (मृधः) संग्राम करनेवाले पापों को (परि जहि) सर्वत्र नष्ट कर दीजिए। (तत्) वह प्रसिद्ध (स्पार्हम्) स्पृहणीय (वसु) सत्य, अहिंसा, आरोग्य, विद्या, सुवर्ण आदि आध्यात्मिक और भौतिक धन (आभर) हमें प्रदान कीजिए ॥१०॥
आ व इन्द्रं कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् । मꣳहिष्ठꣳ सिञ्च इन्दुभिः ॥२१४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 214)
हे साथियो ! (वाजयन्तः) बल, विज्ञान या ऐश्वर्य की इच्छा करते हुए (वः) तुम लोग (शतक्रतुम्) बहुत ज्ञानी और बहुत से कर्मों को करनेवाले, (इन्द्रम्) परमात्मा को (इन्दुभिः) भक्तिरसों से (आ) आसिञ्चित करो। जैसे (वाजयन्तः) अन्नों की उत्पत्ति चाहनेवाले किसान लोग (कृविम्) कृत्रिम कुएँ को खेतों में सिंचाई करने के लिए (इन्दुभिः) जलों से भरते हैं, उसी प्रकार मैं भी (मंहिष्ठम्) अतिशय दानी, सबसे महान् और पूज्यतम उस परमात्मा को (इन्दुभिः) भक्तिरसों से (सिञ्चे) सींचता हूँ ॥१॥
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥२७४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 274)
हे (इन्द्र) शत्रुविदारक परमात्मन् अथवा राजन् ! हम लोग (यतः) जिससे (भयामहे) भय खाते हैं, (ततः) उससे (नः) हमारी (अभयम्) निर्भयता (कृधि) कर दो। हे (मघवन्) निर्भयतारूप धन के धनी! आप (शग्धि) हमें शक्तिशाली बनाओ, (तव) आपका (तत्) वह अभय प्रदान (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिए होवे, आप (द्विषः) द्वेष-वृत्तियों को अथवा द्वेष करनेवालों को (विजहि) विनष्ट कर दो, (मृधः) हिंसावृत्तियों को अथवा आपस के युद्धों को (विजहि) समाप्त कर दो ॥२॥
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ।
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥३११॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 311)
हे (इन्द्र) शूरवीर परमात्मन् वा राजन् ! (त्वम्) आप (प्रतूर्तिषु) झटापटीवाले देवासुरसंग्रामों में (विश्वाः) सब (स्पृधः) स्पर्धालु शत्रु-सेनाओं को (अभि-असि) परास्त करते हो। आप (अशस्तिहा) अप्रशस्ति को दूर करनेवाले, (जनिता) प्रशस्तिप्रद सद्गुणों और सच्चारित्र्यों को हृदय में वा राष्ट्र में उत्पन्न करनेवाले, (वृत्रतूः) पाप वा पापियों की हिंसा करनेवाले (असि) हो। (त्वम्) आप (तरुष्यतः) हिंसकों की (तूर्य) हिंसा करो ॥९॥ इस मन्त्र में अर्थश्लेष और कारण से कार्य का समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है। ‘तूर्’ की तीन बार आवृत्ति तथा तकार की ग्यारह बार आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास अलङ्कार है। परमात्मा और राजा का उपमानोपमेयभाव व्यङ्ग्य है ॥९॥
यो नो वनुष्यन्नभिदाति मर्त उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा ।
क्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥३३६
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 336)
(यः मर्तः) जो मनुष्य (वनुष्यन्) क्रोध करता हुआ (उगणा वा) और सैन्यगणों अथवा आयुध गणों को तैयार किये हुए (मन्यमानः) अभिमान करता हुआ, अथवा (उगणा) अपनी शस्त्रास्त्रों से सज्जित सेनाओं को (मन्यमानः) बहुत मानता हुआ (तुरः) शीघ्रकारी यमराज भी होकर (नः) हमारी (अभिदाति) हिंसा पर उतारू होता है, हे (इन्द्र) शत्रुविदारक परमात्मन् वा राजन्! (तम्) उस मनुष्य को (त्वम्) आप (युधा) युद्ध से (शवसा वा) और बल से (क्षिधि) विनष्ट कर दो। हे (वृषमणः) बलवान् मनवाले परमात्मन् वा राजन्! (त्वोताः) आप से रक्षित हम, उसे (अभिस्याम) परास्त कर दें ॥५॥
अपामीवामप स्रिधमप सेधत दुर्मतिम् । आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥३९७॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 397)
हे (आदित्यासः) शरीरस्थ प्राणो, राष्ट्रस्थ क्षत्रिय राजपुरुषो अथवा आदित्य ब्रह्मचारियो ! तुम शरीर, समाज और राष्ट्र से (अमीवाम्) रोग को (अप) दूर करो, (स्रिधम्) हिंसावृत्ति, शत्रुकृत हिंसा और हिंसक को (अप) दूर करो, तथा (दुर्मतिम्) कुमति को (अप सेधत) दूर करो। साथ ही (नः) हमें (अंहसः) पाप से (युयोतन) पृथक् करो ॥७॥
प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते ।
इन्द्र नृम्णंहि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥४१३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 413)
हे (इन्द्र) जीवात्मन्, राजन् वा सेनापते! तू (प्रेहि) आगे बढ़ (अभीहि) आक्रमण कर, (धृष्णुहि) शत्रुओं का पराभव कर। (ते) तेरे (वज्रः) वज्रतुल्य शत्रुविनाश-सामर्थ्य का अथवा शस्त्रास्त्र-समूह का (न नियंसते) अवरोध या प्रतिकार नहीं किया जा सकता। (ते) तेरा (शवः) बल (नृम्णं हि) तेरे लिए धनरूप है। तू (स्वराज्यम् अनु) स्वराज्य के अनुकूल (अर्चन्) कर्म करता हुआ, (वृत्रम्) पाप एवं शत्रु को (हनः) विनष्ट कर दे, (अपः) शत्रु से प्रतिरुद्ध सत्कर्मसमूह को (जयाः) जीत ले ॥५॥
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम् ।
युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्मां इन्द्र वसौ दधः ॥४१४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 414)
(यत्) जब (आजयः) देवासुरसंग्राम (उदीरते) उपस्थित होते हैं, तब (धृष्णवे) जो शत्रु का पराजय कर सकता है, उसे ही (धनम्) ऐश्वर्य (धीयते) मिलता है। इसलिए हे (इन्द्र) मेरे अन्तरात्मन्, सेनापति अथवा राजन्! तुम (मदच्युता) शत्रुओं के मद को चूर करनेवाले (हरी) ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय रूप घोड़ों को अथवा युद्धरथ को चलाने के साधनभूत जल-अग्नि रूप या वायु-विद्युत् रूप घोड़ों को (युङ्क्ष्व) कार्य में नियुक्त करो। (कम्) किसी को अर्थात् शत्रुजन को (हनः) विनष्ट करो, (कम्) किसी को अर्थात् मित्रजन को (वसौ) ऐश्वर्य में (दधः) स्थापित करो। (अस्मान्) दिव्य कर्मों में संग्लन हम धार्मिक लोगों को (वसौ) ऐश्वर्य में (दधः) स्थापित करो ॥६॥
पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः ।
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥४२८॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 428)
हे वीररसमय मेरे अन्तरात्मन् अथवा वीर पुरुष ! तू (वाजसातये) संग्राम के लिए अर्थात् शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए (उ सु) भली-भाँति (परि प्र धन्व) चारों ओर प्रयाण कर, (सक्षणिः) हिंसक होकर तू (वृत्राणि) आच्छादक पापों पर (परि) चारों ओर से आक्रमण कर। (ऋणयाः) ऋणों को चुकानेवाला होकर तू (द्विषः) लोभ आदि द्वेषियों को (तरध्यै) पार करने के लिए (नः) हमें (ईरसे) प्रेरित कर ॥२॥
पवस्व सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥४३०॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 430)
हे (सोम) रसागार परमेश्वर और राजन्! (अश्वः न) अग्नि, बादल वा सूर्य के समान (निक्तः) शुद्ध, शुद्ध गुण-कर्म-स्वभाववाले और (वाजी) बलवान् आप (महे) महान् (दक्षाय) बल के लिए तथा (धनाय) धन के लिए (पवस्व) हमें पवित्र कीजिए ॥४॥
त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्पत्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम् ।
स ईं ममाद महि कर्म कर्त्तवे महामुरुं सैनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम् ॥४५७॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 457)
प्रथम—सूर्य-चन्द्र के पक्ष में। (त्रिकद्रुकेषु) वायु, बिजली और बादल रूप तीन पदार्थों से युक्त अन्तरिक्षभागों में (महिषः) महान् (तुविशुष्मः) बहुत बलवान् सूर्यरूप इन्द्र (यवाशिरम्) संयुक्त-वियुक्त होनेवाली सूर्यकिरणों से पूर्णता को प्राप्त होनेवाले (सोमम्) चन्द्रमा को (तृम्पत्) तृप्ति प्रदान करता है, और चन्द्रमा (विष्णुना) उस व्याप्तिमान् सूर्य से (सुतम्) उत्पन्न किये किरणसमूह को (यथावशम्) यथेच्छ (अपिबत्) पान करता है। (सः) वह चन्द्रमा में प्रविष्ट सूर्यकिरणसमूह (ईम्) इस चन्द्रमा को (महि) महान् (कर्म) प्राण-प्रदान, चान्द्र मासों के निर्माण आदि कार्य (कर्तवे) करने के लिए (ममाद) हर्षित करता है। (सः) वह (देवः) प्रकाशमान (सत्यः) सत्यनियमवाला (इन्दुः) चन्द्रमा (एनम्) इस (देवम्) प्रकाशक (सत्यम्) सत्य नियमोंवाले (इन्द्रम्) सूर्य का (सश्चत्) सेवन करता रहता है ॥ द्वितीय—गुरु-शिष्य के पक्ष में। (त्रिकद्रुकेषु) ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड रूप तीन सवनोंवाले शिक्षायज्ञों में (महिषः) महान् (तुविशुष्मः) विद्यार्थी का अतिशय प्रतिभा-बल से युक्त आत्मा (तृम्पत्) तृप्ति लाभ करता हुआ (विष्णुना) व्याप्त विद्यावाले आचार्य से (सुतम्) अभिषुत, (यवाशिरम्) व्रतपालनरूप कर्मों से परिपक्व (सोमम्) ज्ञानरस को (यथावशम्) यथेच्छ (अपिबत्) पान करता है। (सः) पान किया हुआ वह ज्ञान-रस (महाम्) विद्या में महान् (उरुम्) विशाल हृष्टपुष्ट शरीरवाले (ईम्) विद्यार्थी के इस आत्मा को (महि) महान् (कर्म) समाजसुधार आदि कर्म (कर्तवे) करने के लिए (ममाद) हर्षित करता। (देवः) दिव्यगुणयुक्त (सत्यः) सत्य (सः) वह (इन्दुः) विद्यारस (देवम्) दिव्यगुणवाले (सत्यम्) सत्यप्रिय (इन्द्रम्) आत्मा को (सश्चत्) निरन्तर प्राप्त होता रहता है ॥१॥
अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम् ॥५१०॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 510)
(सोमः) पवित्र रस का भण्डार परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीवात्मा के (निष्कृतम्) संस्कृत किये हुए हृदयरूप घर में (गच्छन्) जाता हुआ, (मृधः) संग्रामकर्ता पापरूप शत्रुओं को (अपघ्नन्) विध्वस्त करता हुआ और (अराव्णः) अदानशील स्वार्थभावों को (अप) विनष्ट करता हुआ (पवते) पवित्रता प्रदान करता है ॥१४॥
प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना ।
भद्रान्कृण्वन्निन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥५३३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 533)
(सेनानीः) देवजनों का सेनापति (शूरः) शूरवीर सोम नामक परमेश्वर (गव्यन्) दिव्य प्रकाश-किरणों को प्राप्त कराना चाहता हुआ (रथानाम्) शरीररथारोही जीवात्मारूप योद्धाओं के (अग्रे) आगे-आगे (प्रएति) चलता है, इस कारण (अस्य) इसकी (सेना) देवसेना (हर्षते) प्रमुदित एवं उत्साहित होती है। (सखिभ्यः) अपने सखा उपासकों के लिए (इन्द्रहवान्) सेनापति के प्रति की गयी पुकारों को (भद्रान्) भद्र (कृण्वन्) करता हुआ, अर्थात् उपासकों की पुकारों को सफल करता हुआ (सोमः) वीररसपूर्ण परमेश्वर (रभसानि) बल, वेग आदियों को (वस्त्रा) वस्त्रों के समान (आदत्ते) ग्रहण करता है, अर्थात् जैसे कोई वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही वीर परमेश्वर अपने सेनापतित्व का निर्वाह करने के लिए बल, वेग आदि को धारण करता है ॥१॥
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥५९८॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 598)
हे (उग्र) शत्रुओं पर प्रचण्ड (इन्द्र) शत्रुविदारक जगदीश्वर अथवा राजन् ! आप (वाजेषु) संकटों में (सहस्रप्रधनेषु च) और सहस्रों का संहार करनेवाले घोर देवासुर-संग्रामों में (उग्राभिः) उत्कट (ऊतिभिः) रक्षा-शक्तियों से (नः) हम धार्मिकों की (अव) रक्षा कीजिए ॥४॥
ईशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम् ।
स नः स्वर्षदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत् ॥६४६
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 646)
(शक्रः) शक्तिशाली इन्द्र परमेश्वर (हि) निश्चय ही (ईशे) सकल जगत् का अधीश्वर है। (तम्) उसे, हम (ऊतये) रक्षा के लिए (हवामहे) पुकारते हैं। कैसे परमेश्वर को? (जेतारम्) जो सब वस्तुओं को जीत लेनेवाला है, तथा (अपराजितम्) जो स्वयं किसी से पराजित नहीं होता। (सः) वह परमेश्वर (नः) हमें (द्विषः) आन्तरिक तथा बाह्य शत्रु से (अति स्वर्षत्) पार करे। (ऋतुः) ज्ञान, कर्म, शिव संकल्प और यज्ञ, (छन्दः) गायत्री आदि छन्द, (ऋतम्) सत्य और (बृहत्) बृहत् नामक साम हमारे उपकारक हों ॥६॥ ‘त्वामिद्धि हवामहे’ (साम २३४) इस ऋचा पर गाया जानेवाला साम बृहत् साम कहलाता है ॥६॥
इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम् ।
स नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वर्षदति द्विषः ॥६४७
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 647)
(इन्द्रम्) शूरवीर परमैश्वर्यशाली परमेश्वर को हम योगाभ्यासी जन (धनस्य) विवेकख्यातिरूप ऐश्वर्य की (सातये) प्राप्ति के लिए (हवामहे) पुकारते हैं। कैसे परमेश्वर को? (जेतारम्) जो शत्रुओं और विघ्नों का विजेता, तथा (अपराजितम्) करोड़ों भी शत्रुओं एवं विघ्नों से न हारनेवाला है। (सः) वह विजेता परमेश्वर (नः) हमें (द्विषः) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप पञ्च क्लेशों से (अति स्वर्षत्) पार कर दे, (सः) वह अपराजित परमेश्वर (नः) हमें (द्विषः) व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्त्व इन चित्तविक्षेपरूप योगमार्ग के विघ्नों से (अति स्वर्षत्) पार कर दे ॥७॥
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे । पवमान विदा रयिम् ॥७६१॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 761)
प्रथम—परमात्मा के पक्ष में। हे (पवमान) पवित्रताप्रदायक, सर्वान्तर्यामी सोम परमात्मन्! आप (अप तस्थुषः) हमसे दूर स्थित सद्गुणों को (उप शिक्ष) हमारे समीप ले आओ। (शत्रवे) काम, क्रोध आदि शत्रु के लिए (भियसम्) भय (आधेहि) प्रदान करो और हमें (रयिम्) सत्य, अहिंसा, न्याय आदि दिव्य सम्पत्ति (विदाः) प्राप्त कराओ ॥ द्वितीय—राजा के पक्ष में। हे (पवमान) गतिमय, कर्मवीर राजन् ! आप (अप तस्थुषः) हमसे दूर होकर विरोधी पक्ष में स्थित हुए वीरों को (उप शिक्ष) दण्डित करो, (शत्रवे) शत्रु के लिए (भियसम्) भय (आधेहि) उत्पन्न करो और हमें (रयिम्) धन, धान्य, सुवर्ण आदि सम्पत्ति (विदाः) प्राप्त कराओ ॥१॥
शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥८१२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 812)
यह इन्द्र अर्थात् परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा वा विद्या के ऐश्वर्य से युक्त आचार्य (दाशुषे) आत्मसमपर्ण करनेवाले उपासक वा शिष्य के हितार्थ (धृष्णुया) अपने धर्षक गुण से (शतानीका इव) सौ शत्रुसेनाओं के तुल्य (वृत्राणि) उपासक या शिष्य के दोषों पर (प्र जिगाति) आक्रमण करता है और (हन्ति) उन्हें नष्ट कर देता है। (पुरुभोजसः) बहुत पालन करनेवाले (अस्य) इस परमात्मा वा आचार्य के (दत्राणि) दान (पिन्विरे) उपासक वा शिष्य के प्रति प्रवाहित होते हैं, (गिरेः इव रसाः) जैसे पर्वत के जल प्रवाहित हुआ करते हैं ॥२॥
सुवितस्य वनामहेऽति सेतुं दुराय्यम् । साह्याम दस्युमव्रतम् ॥८९३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 893)
हम (सेतुम्) रुकावट को (अति) अतिक्रान्त अर्थात् पार करके (सुवितस्य) सुप्राप्त आनन्द—रसागार परमात्मा के एवं विद्यारसागार आचार्य के (दुराय्यम्) दुष्प्राप्य आनन्दरस वा विद्यारस को (वनामहे) सेवन करते हैं। उससे हम (अव्रतम्) व्रतविरोधी वा सत्कर्मविरोधी (दस्युम्) उपक्षयकारी काम, क्रोध, आदि छहों रिपुओं को (साह्याम) पराजित कर देवें ॥२॥
आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत् । अश्ववत्सोम वीरवत् ॥८९५॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 895)
हे (इन्दो) दीप्तिमान्, ज्ञानरस से भिगोनेवाले (सोम) प्रेरक परमात्मन् वा आचार्य! आप हमारे लिए (गोमत्) श्रेष्ठ गाय से युक्त वा श्रेष्ठ वाणी से युक्त, (हिरण्यवत्) सुर्वण से युक्त, ज्योति से युक्त वा यश से युक्त, (अश्ववत्) घोड़ों से युक्त वा प्राणों से युक्त, (वीरवत्) वीर पुत्रों से युक्त वा वीरभावों से युक्त, (महीम्) बड़ी (इषम्) इच्छासिद्धि को (आ पवस्व) प्राप्त कराइये ॥४॥
पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥८९६॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 896)
हे (विश्वचर्षणे) विश्व ब्रह्माण्ड के द्रष्टा परमात्मन् वा सब विद्याओं के द्रष्टा आचार्य ! आप पवस्व अन्तःप्रकाश एवं ज्ञानरस को प्रवाहित करो। उससे (मही रोदसी) महिमामय आत्मा और मन को (आपृण) पूर्ण कर दो, (न) जैसे (उषाः) उषा और (सूर्यः) सूर्य (रश्मिभिः) किरणों से (मही रोदसी) महान् द्यावापृथिवी को पूर्ण करते हैं ॥५॥
परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम् ॥८९७॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 897)
हे (सोम) रसागार परमात्मन् वा आचार्य! आप (शर्मयन्त्या) सुख देनेवाली (धारया) अध्यात्मप्रकाश की धारा वा ज्ञान की धारा के साथ (विश्वतः) सब ओर से (नः) हमें (परिसर) प्राप्त हों। (रसाइव) जैसे रसीली वर्षा (विष्टपम्) भूलोक को प्राप्त होती है ॥६॥
आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वह्निर्न विश्पतिः ।
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिमपो जिन्वन्गविष्टये धियः ॥१०१२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1012)
हे (सुदक्ष) शुभ योगबल से युक्त आचार्यप्रवर ! (चम्वोः) द्यावापृथिवी के तुल्य परा और अपरा विद्याओं में (सुतः) निष्णात आप (विशाम्) प्रजाओं के (वह्नि) भार को उठानेवाले (विश्पतिः न) प्रजापालक राजा के समान (आ वच्यस्व) प्रशंसा प्राप्त कीजिए, (गविष्टये) दिव्य प्रकाश के इच्छुक मुझ शिष्य के लिए (धियः) प्रज्ञानों को (जिन्वन्) प्रेरित करते हुए आप (दिवः) मूर्धा-लोक से (वृष्टिम्) धर्ममेघ समाधि में होनेवाली ज्योति की वर्षा को और (अपः) आनन्द-जल की (रीतिम्) धारा को (पवस्व) प्रवाहित कीजिए ॥२॥
महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥१२१४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1214)
हे (पवमान) क्रियाशील परमात्मन् वा वीर मनुष्य ! आप (नः) हमारे लिए (महः रायः) महान् धनों को (आभर) लाओ, (मृधः) हिंसक शत्रुओं को (जहि) विनष्ट करो। हे (इन्दो) तेज से प्रदीप्त परमात्मन् वा वीर मनुष्य! आप (वीरवत् यशः) वीरों जैसा यश (रास्व) हमें प्रदान करो ॥२॥
शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाꣳ ऋचीषम । अवा नः पार्ये धने ॥१६४४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1644)
हे (ऋचीषम) वेदवागीशों का मान करनेवाले (इन्द्र) परमैश्वर्यवान् परमात्मा वा जीवात्मा! (पुरु) बहुत (विद्वान्) विद्वान् तुम (नः) हमें (रायः) भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य (आ शिक्ष) प्रदान करो। (पार्ये) मार्ग के पार जाकर प्राप्त करने योग्य (धने) धन के निमित्त (नः) हमारी (अव) रक्षा करो ॥३॥
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते ।
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥१६७६॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1676)
हे जगदीश्वर! (इमे हि) ये (ते) तेरे लिए (ब्रह्मकृतः) स्तोत्र-पाठ करनेवाले उपासक (सुते) उपासना-यज्ञ में (सचा) एक साथ मिलकर (आसते) बैठे हुए हैं, (मधौन) शहद के छत्ते पर जैसे (मक्षः) मधु-मक्खियाँ (सचा) मिलकर (आसते) बैठी होती हैं। (वसूयवः) अध्यात्म धन के इच्छुक (जरितारः) स्तोता गण (इन्द्रे) परमैश्वर्यशाली तुझ जगदीश्वर में (कामम्) अपनी अभिलाषा को (आदधुः) रखे हुए हैं, संजोये हुए हैं, (वसूयवः) भौतिक धन के इच्छुक लोग (रथेन) जैसे रथ में (पादम्) अपना पैर रखते हैं ॥२॥
वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धियः ।
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघां सति ।
या ते रातिर्ददिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥१८०३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1803)
(विश्वाः) सब (अर्यः) आक्रमण करनेवाली; (अरातयः) दान-हीन शत्रुसेनाएँ और विघ्नसेनाएँ (सु) पूर्णरूप से (विनशन्त) विनष्ट हो जाएँ, (नः) हमें (धियः) योग की धारणा, ध्यान और समाधियाँ प्राप्त हों। हे (इन्द्र) जगदीश्वर! (यः) जो शत्रु (नः) हमारा (जिघांसति) वध कर देना चाहता है, उस (शत्रवे) काम, क्रोध आदि शत्रु पर, आप (वधम्) मौत (अस्ता असि) डालनेवाले हो। (या) जो (ते) आपकी (रातिः) दान की प्रवृत्ति है, वह हमारे लिए (वसु) निवासक दिव्य ऐश्वर्य की (ददिः) देनेवाली हो। (अन्यकेषाम्) शत्रुओं की (धन्वसुअधि) धनुषों पर चढ़ायी हुई (ज्याकाः) डोरियाँ (नभन्ताम्)
टूट जाएँ, अर्थात् वे साधनहीन असहाय होकर विनष्ट हो जाएँ ॥३॥
मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः । शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥१८०६॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1806)
हे (इन्द्र) जगदीश्वर! आप (नः) हमें (मा) न तो (पीयत्नवे) हिंसक काम, क्रोध, लोभ आदि के लिए और (मा) न ही (शर्धते) बलवान् किसी मानव शत्रु के लिए (परा दाः) छोड़ो। हे (शचीवः) शक्तिशाली परमात्मन् ! आप (शचीभिः) अपनी शक्तियों से (शिक्ष) हमें शक्तिशाली बनाने की इच्छा करो ॥३॥
असृग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१८१२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1812)
(मैं) इन ब्रह्मानन्द-रूप सोम-रसों को (देववीतये) दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए (असृग्रम्) अपने अन्तरात्मा में प्रवाहित कर रहा हूँ। ये (वाजयन्तः) अन्न प्रदान करते हुए (रथाः इव) रथों के समान (वाजयन्तः) बल प्रदान कर रहे हैं ॥३॥
बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः ।
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम् ॥१८५२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1852)
हे (बृहः पते) दिव्यगुणों की विशाल सेना के अधिपति जीवात्मन् ! (रक्षोहा) पाप वा दुर्जन रूप राक्षसों का वधकर्ता तू (अमित्रान्) विघ्नों और शत्रुओं को (अपबाधमानः) तिरस्कृत करता हुआ (रथेन) शरीर-रथ से (परि दीय) चारों ओर पहुँच। (सेनाः) काम-क्रोध आदि की और दुर्जनों की सेनाओं को (प्रभञ्जन्) तोड़ता-फोड़ता हुआ, (प्रमृणः) हत्यारे दुर्विचारों वा हिंसक मनुष्यों को (युधा) आन्तरिक और बाह्य देवासुरसङ्ग्राम से (जयन्) जीतता हुआ (अस्माकम्) हम सदाचारी, धार्मिक, न्यायकारी जनों के (रथानाम्) रथों का (अविता) रक्षक एधि हो ॥१॥
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित् ॥१८५३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1853)
हे (इन्द्र) जीवात्मन्! (बलविज्ञायः) ब्रह्मबल का ज्ञाता, (स्थविरः) अनुभव में वृद्ध, (प्रवीरः) अतिशय वीर, (सहस्वान्) उत्साही, (वाजी) विज्ञानवान् (सहमानः) सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों को सहन करनेवाला, (उग्रः) प्रतापी, (अभिवीरः) मन, प्राण, आदि वीरों से युक्त, (सहोजाः) बल में प्रसिद्ध, (गोवित्) विवेक की किरणों को और श्रेष्ठ वाणियों को प्राप्त तू (जैत्रम्) विजयशील (रथम्) रथ पर (आतिष्ठ) बैठ ॥२॥
गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा ।
इमं सज़ाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ॥१८५४॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1854)
(गोत्रभिदम्) अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश रूप पर्वतों को तोड़नेवाले, (गोविदम्) विवेक-प्रकाश की किरणों को प्राप्त करनेवाले, (वज्रबाहुम्) अशुद्धि के क्षय तथा ज्ञान की दीप्ति के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूप वज्र को ग्रहण करनेवाले, (अज्म) देवासुरसङ्ग्राम को (जयन्तम्) जीतनेवाले, (अजोसा) बल से (प्रमृणन्तम्) आन्तरिक शत्रुओं को कुचलनेवाले (इमम् अनु) इस जीवात्मा का अनुसरण करके, हे (सज़ाताः) शरीर के साथ उत्पन्न मन, बुद्धि, प्राण, आदियो ! तुम (वीरयध्वम्) वीरता दिखाओ। हे (सखायः) मित्रो! तुम (इन्द्रम् अनु) जीवात्मा का अनुसरण करते हुए (संरभध्वम्) वीरतापूर्ण कार्यों को आरम्भ करो ॥३॥
हे योद्धाओ! शत्रु के किलों के भेदक, गोपालक, वज्र जैसी भुजा वाले, बल से शत्रु का विनाश करने वाले विजेता इंद्र के नेतृत्व में रहकर प्राक्रम दिखाओ। हे मित्रो इंद्र के क्रोध करने पर आप भी शत्रु पर क्रोध करें।
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः ।
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥१८५५॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1855)
(सहसा) आत्मबल से (गोत्राणि) व्याधि, स्त्यान, संशय आदि योग-विघ्नों के तथा बाह्य विघ्नों के किलों का (अभि गाहमानः) अवगाहन करता हुआ, (अदयः) आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुओं पर दया न दिखानेवाला, (वीरः) वीर, (शतमन्युः) अनन्त तेजवाला, (दुश्च्यवनः) शत्रुओं से विचलित न किया जा सकनेवाला, (पृतनाषाट्) शत्रुसेनाओं को पराजित कर देनेवाला, (अयुध्यः) शत्रुओं के लिए जिससे युद्ध कर पाना असम्भव होता है ऐसा (इन्द्रः) जीवात्मा-रूप सेनापति (युत्सु) आन्तरिक तथा बाह्य देवासुरसङ्ग्रामों में (अस्माकं सेनाः) हमारी यम-नियम आदि की सेनाओं को और धार्मिक योद्धाओं की सेनाओं को (प्र अवतु) भली-भाँति रक्षित करे ॥१॥
बल से शत्रु किलों के भेदनेवाले, प्राक्रमी, शत्रुपर दया न करने वाले वीर, अनीति के प्रति क्रोध करने वाले, अविचल, शत्रु विजेता, अद्वितीय योद्धा, ऐसे इंद्र देव हमारी सेना का संरक्षण करें।
इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् ॥१८५६॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1856)
(बृहः पतिः) महान् शरीर-रूप राष्ट्र का रक्षक (इन्द्रः) वीर जीवात्मा-रूप सेनापति (आसाम्) इन देव-सेनाओं का (नेता) नेता हो। (दक्षिणा) त्याग की भावना, (यज्ञः) परमेश्वरपूजारूप यज्ञ (सोमः) और शान्ति का व्रत (पुरः एतु) आगे-आगे चले। (अभिभञ्जतीनाम्) अदिव्य भावों तथा अधार्मिक दुष्ट-जनों को तोड़ती-फोड़ती-कुचलती हुई, (जयन्तीनाम्), विजय का उत्कर्ष प्राप्त करती हुई (देवसेनानाम्) दिव्यभावों तथा सदाचारी विद्वान् जनों की सेनाओं के (अग्रम्) आगे-आगे (मरुतः) प्राण तथा वायुवत् बलिष्ठ शूरवीर लोग (यन्तु) चलें ॥२॥
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताꣳ शर्ध उग्रम् ।
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् ॥१८५७॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1857)
(वृष्णः) महाबली (इन्द्रस्य) विघ्नविदारक जीवात्मा का, (राज्ञः) सङ्कल्प बल से राजित (वरुणस्य) श्रेष्ठ मन का और (आदित्यानाम्) दोषापहारी (मरुताम्) प्राणों का (उग्रम्) उग्र (शर्धः) बल (उदस्थात्) हमारे सहायक हों। (महामनसाम्) बड़े हौसलेवाले, (भुवनच्यवानाम्) शत्रुनगरों के विध्वंसक, (जयताम्) विजय-लाभ करनेवाले (देवानाम्) दिव्य भावों का और धर्मात्मा रण-बाँके वीरों का (घोषः) विजय-घोष (उदस्थात्) ऊपर उठे ॥३॥
उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनाꣳसि ।
उद्वृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१८५८॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1858)
हे (मघवन्) शरीर के अधिष्ठाता ऐश्वर्यशाली जीवात्मन्! (आयुधानि) शस्त्रास्त्रों को (उद्धर्षय) ऊपर उठाओ, (मामकानाम्) मेरे (सत्वनाम्) वीरों के (मनांसि) मनों को (उत्) ऊपर उठाओ, उत्साहित करो। हे (वृत्रहन्) पापहन्ता, विघ्नहन्ता, शत्रुहन्ता जीवात्मन्! (वाजिनाम्) बलवान् योद्धाओं के (वाजिनानि) रण-कौशल (उद्यन्तु) ऊपर उठें, (जयताम्) विजय-लाभ करते हुए (रथानाम्) रथारोहियों के (घोषाः) विजय-घोष (उद् यन्तु) ऊपर उठें ॥१॥
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु ।
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माꣳ उ देवा अवता हवेषु ॥१८५९॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1859)
(अस्माकम् इन्द्रः) हमारा सेनापति-तुल्य जीवात्मा (ध्वजेषु समृतेषु) हमारे ध्वजों के शत्रु-ध्वजों से टकराने पर (जयतु) विजय-लाभ करे। (अस्माकं याः इषवः) हमारे जो बाण हैं, (ताः जयन्तु) वे विजय-लाभ करें। (अस्माकं वीराः) हमारे रण-कुशल वीर योद्धा (उत्तरे भवन्तु) विजयी हों। हे (देवाः) जीतने के अभिलाषी मन, बुद्धि आदियो! (अस्मान् उ) हमारी (हवेषु) देवासुरसङ्ग्रामों में (अवत) रक्षा करो ॥२॥
असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना ।
तां गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात् ॥१८६०॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1860)
हे (मरुतः) प्राणो वा वीर सैनिको! (असौ या) यह जो (ओजसा) अपने बल से (स्पर्धमाना) हमसे स्पर्धा करती हुई (परेषाम्) शत्रुओं की (सेना) सेना (नः अभ्येति) हमारी ओर बढ़ी आ रही है, (ताम्) उस सेना को (अपव्रतेन) जिसमें कार्य बन्द हो जाते हैं, ऐसे (तमसा) अन्धकार से (गूहत) आच्छन्न कर दो, (यथा) जिससे (एतेषाम्) इनमें (अन्यः) एक (अन्यम्) दूसरे को (न जानात्) न जान सके ॥३॥
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि ।
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥१८६१॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1861)
हे (अप्वे) व्याधि वा भीति! (परेहि) शत्रुदल में जा। (अमीषाम्) इन शत्रुओं के (चित्तम्) चित्त को (मोहयन्ती) मोहित करती हुई (अङ्गानि) इनके अङ्गों को (गृहाण) जकड़ दे। (अभिप्रेहि) शत्रुओं के प्रति जा, उनके (हृत्सु) हृदयों में (शोकैः) शोकों से (निर्दह) दाह उत्पन्न कर दे। (अमित्राः) शत्रु (अन्धेन) घने (तमसा) मोह के अन्धकार से (सचन्ताम्) संयुक्त हो जाएँ ॥१॥
अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि । उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥१८६५॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1865)
हे (मघवन्) दिव्य ऐश्वर्यवाले, (वृत्रहन्) शत्रुहन्ता (इन्द्र) वीर जीवात्मन् ! (अस्मान् अभि) हमारे प्रति (शत्रुयतीम्) शत्रुता का आचरण करनेवाली (ताम्) उस विकराल (अमित्रसेनाम्) रिपु-सेना को, तू (अग्निः च) और तैजस मन (उभौ) दोनों (प्रतिदहतम्) भस्म कर दो ॥२॥
वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥१८६७॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1867)
हे (वृत्रहन् इन्द्र) पापहन्ता जीवात्मन् और शत्रुहन्ता सेनापति! तुम (रक्षः) राक्षसी स्वभाव को वा राक्षसी स्वभाववाले दुर्जन को (विजहि) विनष्ट करो, (मृधः) सङ्ग्रामकारी काम-क्रोध आदियों को वा हिंसक मानवी शत्रुओं को (विजहि) विनष्ट करो, (वृत्रस्य) पुण्य पर पर्दा डालनेवाले पाप वा पापी के (हनू) आक्रमण और बचाव के उपायों को वा जबड़ों को (विरुज) चूर-चूर कर दो। (अभिदासतः) दंशन-छेदन-भेदन करनेवाले (अमित्रस्य) शत्रु के (मन्युम्) प्रदीप्त-प्रभाव को वा क्रोध को (वि) विध्वस्त कर दो ॥१॥
वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥१८६८॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1868)
हे (इन्द्र) जीवात्मन् वा सेनापति! तुम (नः) हमारे (मृधः) हिंसकों को (विजहि) विनष्ट करो, (पृतन्यतः) सेना से आक्रमण करनेवाले काम-क्रोध आदि को वा बाहरी शत्रुओं को (नीचा यच्छ) नीचा दिखाओ। (यः) जो आन्तरिक वा बाहरी शत्रु (अस्मान्) हम धार्मिकों को (अभिदासति) सर्वथा क्षीण करना चाहता है, उसे (अधरं तमः गमय) घोर दुर्गति प्राप्त कराओ वा निचले कारागार में डाल दो ॥२॥
अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव । तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥१८७१
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1871)
हे (अमित्राः) आन्तरिक और बाह्य शत्रुओ! तुम (अन्धाः) अन्धे और (अशीर्षाणः अहयः इव) फन-कटे साँपों के समान प्रभाव-रहित (भवत) हो जाओ। (अग्निनुन्नानां तेषां वः) अग्नि के समान ज्वलन्त दृढ सङ्कल्प से दूर किये हुए उन तुम शत्रुओं में से (वरं-वरम्) प्रधान-प्रधान को चुन-चुन कर (इन्द्रः) हमारा अन्तरात्मा (हन्तु) विनष्ट कर दे ॥२॥
यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति ।
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरम् ॥१८७२॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1872)
(यः) जो (नः) हमें (स्वः) अपना दुर्भाव, (अरणः) पराया दुर्भाव, (यः च) और जो (निष्ठ्यः) शत्रु का दुर्भाव (जिघांसति) नष्ट करना चाहता है, (तम्) उस काम-क्रोध आदि दुर्भाव का (सर्वे) सब (देवाः) दिव्यगुण वा सदाचारी विद्वान् जन (धूर्वन्तु) वध कर दें। (ब्रह्म) महान् जगदीश्वर (मम) मेरा (अन्तरम्) आन्तरिक (वर्म) कवच अर्थात् रक्षा-साधन हो जाए, (शर्म) जगदीश की शरण (मम) मेरा (अन्तरम्) आन्तरिक (वर्म) कवच अर्थात् रक्षा-साधन हो जाए ॥३॥
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः ।
सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृधो नुदस्व ॥१८७३॥
(सामवेद - मन्त्र संख्या : 1873)
हे (इन्द्र) वीर मानव ! तू (भीमः) भयङ्कर, (कुचरः) भूमि पर विचरनेवाले, (गिरिष्ठाः) पर्वत की गुफा में निवास करनेवाले (मृगः न) शेर के समान (भीमः) दुष्टों के लिए भयङ्कर, (कुचरः) भू-विहारी और (गिरिष्ठाः) पर्वत के सदृश उन्नत पद पर प्रतिष्ठित हो। (परावतः) सुदूर देश से (परस्याः) और दूर दिशा से (आ जगन्थ) शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए आ। (सृकम्) गतिशील, (तिग्मम्) तीक्ष्ण (पविम्) वज्र को, शस्त्रास्त्रसमूह को (संशाय) और अधिक तीक्ष्ण करके (शत्रून्) शत्रुओं को (वि ताढि) विताड़ित कर, (मृधः) हिंसकों को (वि नुदस्व) दूर भगा दे ॥१॥
हिन्दी अनुवादः स्वामी दयानन्द सरस्वती
(स्वामी दयानन्द सरस्वती के संस्कृत भाष्य के आधार पर)
अथर्ववेद
अथर्ववेद में युद्ध का विषय बहुत आया है। इनमें से कुछ मंत्र यहां उद्धृत हैं:
त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धाँ इहा वह।
अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 7; मन्त्र » 7)
(अग्ने) हे अग्नि! (त्वम्) तू (उप बद्धान्) दृढ़ बाँधे हुए (यातुधानान्) दुःखदायी राक्षसों को (इह) यहाँ पर (आवह) ले आ। (अथ) और (इन्द्रः) वायु (वज्रेण) कुल्हाड़े से (एषाम्) इनके (शीर्षाणि) मस्तकों को (अपि) भी (व्रश्चतु) काट डाले ॥७॥
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च।
नि स्तुवानस्य पातय परमक्ष्युतावरम् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 8; मन्त्र » 3)
(सोमप) हे अमृत पीने हारे [राजन्]! तू (यातुधानस्य) पीड़ा देनेहारे पुरुष के (प्रजाम्) मनुष्यों को (जहि) मार, (च) और (नयस्व) ले आ। (निस्तुवानस्य) अपस्तुति [निन्दा] करते हुए [शत्रु की] (परम्) उत्तम [हृदय की] (उत) और (अवरम्) नीची [शिर की] (अक्षि) आँख को (पातय) निकाल दे ॥३॥
यस्ते मन्योऽविधद्वज्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्।
साह्याम दासमार्यं त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥
अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्तपसा युजा वि जहि शत्रून्।
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 4; सूक्त » 32; मन्त्र » 1,3)
(वज्र) हे वज्ररूप (सायक) हे शत्रुनाशक (मन्यो) दीप्तिमान् क्रोध! (यः) जिस पुरुष ने (ते) तेरी (अविधत्) सेवा की है, वह (विश्वम्) सब (सहः) शरीरबल और (ओजः) समाजबल (आनुषक्) लगातार (पुष्यति) पुष्ट करता है। (सहस्कृतेन) बल से उत्पन्न हुए, (सहस्वता) बलवान्, (त्वया युजा) तुझ सहायक के साथ (सहसा) बल से (वयम्) हम लोग (दासम्) दास, काम बिगाड़ देनेवाले मूर्ख और (आर्यम्) आर्य अर्थात् विद्वान् का (सह्याम) निर्णय करें ॥१॥ (मन्यो) हे प्रकाशमान क्रोध (तवसः) महान् से भी (तवीयान्) अति महान् तू (अभीहि) इधर आ, (तपसा युजा) अपने ऐश्वर्य, मित्र के साथ (शत्रून्) शत्रुओं को (विजहि) मिटा दे। (च) और (अमित्रहा) पीड़ा देनेवालों का मारनेवाला, (वृत्रहा) अन्धकार नाश करनेवाला, (दस्युहा) डाकुओं का मारनेवाला (त्वम्) तू (विश्वा) सब (वसूनि) धनों को (नः) हमारे लिये (आ) सब ओर से (भर) भर दे ॥३॥
तान्त्सत्यौजाः प्र दहत्वग्निर्वैश्वानरो वृषा।
यो नो दुरस्याद्दिप्साच्चाथो यो नो अरातियात् ॥
यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति।
वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोरग्नेरपि दधामि तम् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 4; सूक्त » 36; मन्त्र » 1,2)
(सत्यौजाः) सत्य बलवाला, (वैश्वानरः) सब नरों का हित करनेवाला, (वृषा) सुख वर्षानेवाला वा ऐश्वर्यवान् (अग्निः) सर्वव्यापक परमेश्वर (तान्) उन सबको (प्रदहतु) भस्म कर डाले। (यः) जो (नः) हमें (दुरस्यात्) दुष्ट माने, (च) और जो (दिप्सात्) मारना चाहे, (अथो) और भी (यः) जो (नः) हम से (अरातियात्) बैरी सा बर्ताव करे ॥१॥ (यः) जो पुरुष (अदिप्सतः) न सतानेवाले (नः) हमको (दिप्सत्) सताना चाहे, (च) और (यः) जो (दिप्सतः) सतानेवाले [हम] को (दिप्सति) सताना चाहता है, (तम्) उसको (वैश्वानरस्य) सब नरों के हितकारक (अग्नेः) ज्ञानीपुरुष के (दंष्ट्रयोः) दोनों डाढ़ों के बीच जैसे (अपि) अवश्य (दधामि) धरता हूँ ॥२॥
सहे पिशाचान्त्सहसैषां द्रविणं ददे।
सर्वान्दुरस्यतो हन्मि सं म आकूतिरृध्यताम् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 4; सूक्त » 36; मन्त्र » 4)
(पिशाचान्) मांसभक्षकों को (सहसा) बल से (सहे) मैं जीतता हूँ, और (एषाम्) इनका (द्रविणम्) धन [सुपात्रों को] (ददे) मैं देता हूँ। (दुरस्यतः) सतानेवाले (सर्वान्) सबों को (हन्मि) मैं मारता हूँ। (मे) मेरा (आकूतिः) शुभ संकल्प (सम् ऋध्यताम्) यथावत् सिद्ध होवे ॥४॥
रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत्पिशाचाः पृष्टीर्वोऽपि शृणातु यातुधानाः।
वीरुद्वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत् ॥
अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोऽर्चिषात्त्रिणो नुदतं प्रतीचः।
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 6; सूक्त » 32; मन्त्र » 2,3)
(पिशाचाः) हे मांसभक्षक! ख्रोगो वा प्राणियो, (रुद्रः) दुःखनाशक सेनापति ने (वः) तुम्हारे (ग्रीवाः) गले को (अशरैत्) तोड़ डाला है, (यातुधानाः) हे पीड़ादायको! (वः) तुम्हारी (पृष्टीः) पसलियाँ (अपि) भी (शृणातु) तोड़े। (विश्वतोवीर्या) सब ओर से सामर्थ्यवाली (वीरुत्) विविध प्रकार से प्रकाशित होनेवाली शक्ति ख्परमेश्वर, ने (वः) तुमको (यमेन) नियम के साथ (सम् अजीगमत्) संयुक्त किया है ॥२॥ (मित्रावरुणौ) हे प्राण और अपान! ख्अथवा हे दिन और रात्रि !, (नः) हमारे लिये (इह) यहाँ पर (अभयम्) अभय (अस्तु) होवे, ख्तुम दोनों अपने, (अर्चिषा) तेज से (अत्त्रिणः) खा डालनेवालों को (प्रतीचः) उलटा (नुदतम्) हटा दो। वे लोग (मा) न तो (ज्ञातारम्) सन्तोषक पुरुष को और (मा) न (प्रतिष्ठाम्) प्रतिष्ठा को (विदन्त) पावें, (मिथः) आपस में (विघ्नानाः) मारते हुए (मृत्युम्) मृत्यु को (उपयन्तु) प्राप्त हों ॥३॥
निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैषां म्लापयामसि।
अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहै ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 6; सूक्त » 66; मन्त्र » 3)
(शत्रवः) शत्रु लोग (निर्हस्ताः) निहत्थे (सन्तु) हो जावें, (तेषाम्) उन के (अङ्गा) अङ्गों को (म्लापयामसि) हम शिथिल करते हैं। (अथ) फिर (इन्द्र) हे महाप्रतापी सेनापति इन्द्र! (तेषाम्) उन के (वेदांसि) सब धनों को (शतशः) सैकड़ों प्रकार से (वि भजामहै) हम बाँट लेवें ॥३॥
ऐषु नह्य वृषाजिनं हरिणस्या भियं कृधि।
पराङमित्र एषत्वर्वाची गौरुपेषतु ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 6; सूक्त » 67; मन्त्र » 3)
[हे सेनापति!] (एषु) इन [अपने वीरों] में (वृषा=वृष्णः) ऐश्वर्यवान् पुरुष का (अजिनम्) चर्म [कवच] (आ नह्य) पहिना दे, और [शत्रुओं में] (हरिणस्य) हरिण का (भियम्) डरपोकपन (कृधि) कर दे। (अमित्रः) शत्रु (पराङ्) उलटे मुख होकर, (एषतु) चला जावे (गौः) भूमि [युद्धभूमि और राज्य] (अर्वाची) हमारी ओर (उप एषतु) चली आवे ॥३॥
वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहै।
म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 7; सूक्त » 90; मन्त्र » 2)
(वयम्) हम लोग (इन्द्रेण) बड़े ऐश्वर्यवाले राजा के साथ (अस्य) इस [शत्रु] के (संभृतम्) एकत्र किये हुए (तत्) उस (वसु) धन को (वि भजामहै) बाँट लेवें। [हे शत्रु!] (वरुणस्य) शत्रुनिवारक राजा की (व्रतेन) व्यवस्था से (ते) तेरी (भ्रजः) तमक और (शिभ्रम्) ढिठाई को (म्लापयामि) मैं मेटता हूँ ॥२॥
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम्।
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 8; सूक्त » 3; मन्त्र » 4)
(अग्ने) हे अग्नि [समान तेजस्वी राजन्!] (यातुधानस्य) दुःखदायी दुष्ट की (त्वचम्) खाल (भिन्धि) उजाड़ दे, [तेरी] (हिंस्रा) वध करनेवाली (अशनिः) बिजुली [बिजुली का वज्र] (हरसा) अपने तेज से (एनम्) इस [अत्याचारी] को (हन्तु) मारे। (जातवेदः) हे महाधनी राजन्! [उसके] (पर्वाणि) जोड़ों को (प्र शृणीहि) कुचल डाल, (क्रव्यात्) मांस खानेवाला, (क्रविष्णुः) भयंकर [सिंह, गीदड़, गिद्ध आदि जीव] (एनम्) इसको (वि चिनोतु) चींथ डाले ॥४॥
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्।
उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 8; सूक्त » 3; मन्त्र » 5)
(जातवेदः) हे प्रसिद्ध ज्ञानवाले! (अग्ने) हे अग्नि ख्समान प्रतापी राजन्!, (यत्र) जहाँ कहीं (इदानीम्) अब (तिष्ठन्तम्) खड़े हुए, (उत) और (वा) अथवा (चरन्तम्) घूमते हुए (उत) और (अन्तरिक्षे) आकाश में ख्विमान आदि से, (पतन्तम्) उड़ते हुए (यातुधानम्) दुःखदायी जन को (पश्यसि) तू देखता है, (शिशानः) तीक्ष्णस्वभाव, (अस्ता) बाण चलानेवाला तू (शर्वा) बाण वा वज्र से (तम्) उसे (विध्य) वेध ले ॥५॥
यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनिभिर्दिहानः।
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्प्रतीचो बाहून्प्रति भङ्ग्ध्येषाम् ॥
उतारब्धान्त्स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणाँ ऋष्टिभिर्यातुधानान्।
अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा।
तस्याग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 8; सूक्त » 3; मन्त्र » 6,7,10)
(अग्ने) हे अग्नि ख्समान तेजस्वी राजन्!, (वाचा) वाणी ख्विद्या, द्वारा (यज्ञैः) संयोग-वियोग व्यवहारों से (इषूः) बाणों को (संनममानः) सीधा करता हुआ, और (अशनिभिः) बिजुलियों से (शल्यान्) ख्उनके, शिरों को (दिहानः) पोतता हुआ ख्तीक्ष्ण करता हुआ, तू (ताभिः) उन ख्बाणों, से (यातुधानान्) दुःखदायी जनों को (हृदये) हृदय में (विध्य) वेधले और (एषाम्) उनकी (बाहून्) भुजाओं को (प्रतीचः) उलटा करके (प्रति भङ्ग्धि) तोड़ दे ॥६॥ (उत) और (जातवेदः) हे प्रसिद्धधनवाले राजन् ! (आरब्धान्) ख्शत्रुओं करके, पकड़े हुओं को (स्पृणुहि) पाल (उत) और (अग्ने) हे अग्नि ख्समान तेजस्वी राजन्!, (पूर्वः) सब से पहिले और (शोशुचानः) अति प्रकाशमान तू (आरेभाणान्) ख्हमें, पकड़नेवाले (यातुधानान्) दुःखदायियों को (ऋष्टिभिः) दो धारा तरवारों से (नि जहि) मार डाल, (आमादः) मांस खानेवाली (एनीः) चितकबरी, (क्ष्विङ्काः) अव्यक्त शब्द बोलनेवाली ख्चील आदि पक्षी, (तम्) हिंसक चोर को (अदन्तु) खा जावें ॥७॥ (नृचक्षाः) मनुष्यों पर दृष्टि रखनेवाला तू (रक्षः) राक्षस को (विक्षु) मनुष्यों के बीच (परि पश्य) जाँच कर देख, (तस्य) उसके (त्रीणि) तीन (अग्रा) अग्रभाग ख्मस्तक और दो कंधे, (प्रति शृणीहि) तरेड़ दे। (अग्ने) हे अग्नि ख्समान तेजस्वी राजन् !, (तस्य) उसकी (पृष्टीः) पसलियाँ (हरसा) बल से (शृणीहि) कुचल डाल, (यातुधानस्य) दुःखदायी की (मूलम्) जड़ को (त्रेधा) तीन प्रकार से ख्दोनों जङ्घा और कटिभाग से, (वृश्च) काट दे ॥१०॥
एवा त्वं देव्यघ्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः ॥
वज्रेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुरभृष्टिना ॥
प्र स्कन्धान्प्र शिरो जहि ॥
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेष्टय ॥
मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य सं वृह ॥
अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि ॥
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्रथय ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 12; सूक्त » 5; मन्त्र » 65-71)
(देवि) हे देवी! ख्उत्तम गुणवाली,, (अघ्न्ये) हे अवध्य ! ख्न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी, (त्वम्) तू (एव) इसी प्रकार (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, (कृतागसः) अपराध करनेवाले, (देवपीयोः) विद्वानों के सतानेवाले, (अराधसः) अदानशील पुरुष के ॥६५॥ (शतपर्वणा) सैकड़ों जोड़वाले, (तीक्ष्णेन) तीक्ष्ण, (क्षुरभृष्टिना) छुरे की सी धारवाले (वज्रेण) वज्र से ॥६६॥, (स्कन्धान्) कन्धों और (शिरः) शिर को (प्र प्र जहि) तोड़-तोड़ दे ॥६७॥ (अस्य) उस ख्वेदविरोधी, के (लोमानि) लोमों को (सं छिन्धि) काट डाल, (अस्य) उसकी (त्वचम्) खाल (वि वेष्टय) उतार ले ॥६८॥ (अस्य) उसके (मांसानि) मांस के टुकड़ों को (शातय) बोटी-बोटी कर दे, (अस्य) उसके (स्नावानि) नसों को (सं वृह) ऐंठ दे ॥६९॥ (अस्य) उसकी (अस्थीनि) हड्डियाँ (पीडय) मिसलडाल, (अस्य) उसकी (मज्जानम्) मींग (निर्जहि) निकाल दे ॥७०॥ (अस्य) उसके (सर्वा) सब (अङ्गा) अङ्गों और (पर्वाणि) जोड़ों को (वि श्रथय) ढीला कर दे ॥७१॥
इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमर्कैर्विदद्वसुर्दयमानो वि शत्रून्।
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे ॥
महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि।
वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यूँरभिभूत्योजाः ॥
ससानात्याँ उत सूर्यं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम्।
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्प्रार्यं वर्णमावत् ॥
(अथर्ववेद - काण्ड » 20; सूक्त » 11; मन्त्र » 1,6,9)
(विदद्वसुः) ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषों से युक्त (पूर्भित्) [शत्रुओं के] गढ़ों को तोड़नेवाले, (शत्रून्) वैरियों को (वि) विविध प्रकार (दयमानः) मारते हुए (इन्द्रः) इन्द्र [बड़े ऐश्वर्यवाले राजा] ने (अर्कैः) पूजनीय विचारों से (दासम्) दास [सेवक] को (आ अतिरत्) बढ़ाया है। (ब्रह्मजूतः) ब्रह्माओं [महाविद्वानों] से प्रेरणा किये गये, (तन्वा) उपकार शक्ति से (वावृधानः) बढ़ते हुए, (भूरिदात्रः) बहुत से अस्त्र-शस्त्रवाले [शूर] ने (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और भूमि को (आ) भले प्रकार (अपृणत्) तृप्त किया है ॥१॥ (महः) महान् लोग (अस्य) इस (इन्द्रस्य) इन्द्र [महाप्रतापी राजा] के (सुकृता) धर्म से किये हुए (पुरूणि) बहुत से (महानि) महान् [पूजनीय] (कर्म) कर्मों को (पनयन्ति) सराहते हैं। (अभिभूत्योजाः) हरा देनेवाले बल से युक्त [शूर] ने (वृजिनान्) पापी (दस्यून्) साहसी चोरों को (वृजनेन) बल के साथ (मायाभिः) बुद्धियों से (सं पिपेष) पीस डाला ॥६॥ (इन्द्रः) इन्द्र [महाप्रतापी पुरुष] ने (अत्यान्) घोड़ों को (ससान) सेवा है (उत) और (सूर्यम्) सूर्य [समान प्रतापी वीर] को (ससान) सेवा है, (पुरुभोजसम्) बहुत पालन करनेवाली (गाम्) पृथिवी [वा गौ] को (ससान) सेवा है। (हिरण्ययम्) सुवर्ण (उत) और (भोगम्) भोग [उत्तम पदार्थों के उपयोग] को (ससान) सेवा है, (दस्यून्) साहसी चोरों को (हत्वी) मारकर (वर्णम्) स्वीकार करने योग्य (आर्यम्) आर्य [श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष] की (प्र आवत्) रक्षा की है ॥९॥
वेदों की युद्ध से जुड़ी शिक्षाओं पर एक नज़र
ऊपर युद्ध सम्बन्धी चारों वेदों के मन्त्रों का अक्षरश: उल्लेख कर दिया गया है। उनके यथार्थ भाव को स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक विषय के अनेक मन्त्रों को उद्धृत किया गया है। इनके अध्ययन से जो मुख्य बिंदु उजागर होते हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:
1. आर्यों का युद्ध एक ऐसी जाति से था, जो रंग, नस्ल, धर्म और मातृभूमि में उनसे भिन्न थी, आर्यों ने उनके देश पर आक्रमण किया था और उनके स्थान पर बसना चाहते थे।
2. वे उस जाति को भूत-प्रेत, दैत्य और दुष्टात्माओं में से समझते थे। उन्हें दास, दस्यु, राक्षस, और पिशाच आदि घृणित नामों से पुकारते थे। वे उन्हें मानवता से बाहर, बुद्धि और चेतना से रहित और आर्य जाति की तुलना में हीन और तुच्छ समझते थे। इन्हीं विचारों के तहत उन्होंने अपने दुश्मनों को वह दर्जा देने से इनकार कर दिया जो बराबरी के एक मानव समुदाय को दिया जाना चाहिए।
3. उनकी दृष्टि में युद्ध का कोई उच्च नैतिक उद्देश्य नहीं था। वे धन और सम्पत्ति चाहते थे, वे गायों, बैलों, घोड़ों और अन्य प्रकार के पशुओं की बहुतायत चाहते थे। वे उपजाऊ भूमि और आरामदायक घरों और समृद्धि और भोजन के इच्छुक थे। उनके भीतर राज्यों को पराजित करने की, अपने साथ वालों के बीच वीरता में नाम पाने और देशों पर ऐस्वर्य और विलास के साथ शासन करने की इच्छा पाई जाती थी। वेदों में कहीं भी हमें युद्ध का इससे अच्छा और उच्च उद्देश्य नहीं मिलता।
4. ग़ैर-आर्यों के साथ उनका युद्ध किसी हल होने योग्य विवाद पर आधारित नहीं था, बल्कि एक ऐसे विवाद पर आधारित था जो किसी एक पक्ष के पूर्णतः मिट जाने या पराजित हो जाने के सिवा किसी अन्य परिणाम पर समाप्त नहीं हो सकता था। उनका युद्ध इसी तथ्य पर आधारित था कि वे जातियां आर्य नहीं थीं और आर्यों के देवताओं की पूजा नहीं करती थीं। पहले कारण का ख़त्म हो जाना तो असंभव था क्योंकि नस्ल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बदला जा सके। रहा दूसरा कारण तो वह भी दूर नहीं हो सकता था, क्योंकि आर्यों का धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं था, जिसका प्रचार-प्रसार हो । वेदों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि आर्यों ने ग़ैर-आर्यों को कभी अपने धार्मिक विश्वास और पंथ में आमंत्रित किया हो और उनके सामने यह बात प्रस्तुत की हो कि अगर तुम अमुक नियम और सिद्धांत स्वीकार कर लो तो हम तुम्हें अपने समाज में समानता का अधिकार देकर स्वीकार कर लेंगे। इसके विपरीत हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आर्य वर्ण के लोग ग़ैर-आर्य लोगों को स्वभाव से ही हीन और अपवित्र मानते थे और उनको धार्मिक पूजा में भाग लेने यहां तक कि धार्मिक पुस्तकों को छूने के योग्य भी नहीं समझते थे। यही कारण है कि इन दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच युद्ध तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि देश के मूल निवासी शूद्र बनकर रहने या जंगलों और पहाड़ों में शरण लेने के लिए विवश न कर दिए गए।
5. वेदों के मन्त्रों से यह तो ज्ञात नहीं होता कि आर्य आक्रमणकारियों ने युद्ध में अपने शत्रुओं के साथ वास्तव में कैसा व्यवहार किया था, परन्तु यह निश्चित है कि उनकी उन लोगों को कठोर दण्ड देने की इच्छा थी। जीवित मनुष्य की खाल उधेड़ना, उसके अंगों को काटना, उसे आग में जलाना, उसके टुकड़े-टुकड़े कर देना, हिंसक पशुओं से उसको फड़वा देना, उसे पशुओं की खाल में सी देना, उसके बाल-बच्चों तक का वध कर डालना, ये वे वांछित दंड हैं जिनकी वे कामना करते थे और चाहते थे कि उनके देवता उनके शत्रुओं को दें। जिन के हृदय में ये लालसाएँ पल-बढ़ रही थीं, उनके कार्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
गीता का युद्ध दर्शन
हिंदू धर्म में गीता की महानता मुख्य रूप से श्रीकृष्ण जैसे प्रमुख धार्मिक नेता के कारण है। श्री बालगंगाधर तिलक के अनुसार, यह “भागवद-धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जिस स्पष्टता और विस्तार के साथ यह हिंदू धर्म के दर्शन को उजागर करता है, वह पूरे संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है। यों तो इसमें हिंदू धर्म-दर्शन के बीसियों विषयों पर चर्चा की गई है, लेकिन इसका मुख्य फोकस युद्ध पर है। यह एक हतोत्साहित सैनिक को युद्ध के लिए प्रेरित करने और उसके रक्तपात से घृणा करने वाले हृदय में युद्ध का उत्साह पैदा करने के लिए लिखा गया है।
भारत के इतिहास की यह प्रसिद्ध घटना है कि जब भारत में प्राचीन आर्य सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तब हस्तिनापुर के राजपरिवार में धन और सत्ता की लालसा ने फूट डाल दी। कौरव और पांडव दो विरोधी पक्ष बन गए और दोनों के समर्थन में भारत के महान सरदार खड़े हो गए। पहले तो समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में दोनों पक्षों ने तलवारें निकाल लीं और रणभूमि में भाग्य का फ़ैसला करने के लिए एकत्र हो गए। कृष्णजी उस युद्ध में पांडवों के सहयोगी थे। पांडवों के प्रमुख अर्जुन उनके शिष्य थे। उनकी सेना का जीत के गणतव्य तक मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं कृष्णजी उनके सारथी बन गए। रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने-सामने खड़ी हो गईं और अर्जुन ने अपनी आंखों से अपने मित्रों, स्वजनों और भाइयों को युद्ध के लिए तैयार देखा, तो उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। प्रेम की कोमल भावनाओं से प्रेरित होकर, उन्होंने युद्ध छोड़ने का फ़ैसला किया, तब कृष्णजी ने उन्हें एक लंबा उपदेश दिया, जिसमें युद्ध के दर्शन और उसके विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। यह उपदेश भागवत गीता है।
इस उपदेश का प्रारम्भ इस तरह होता है कि जब अर्जुन का हृदय अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से विमुख होने लगा, तो उसने दुखी होकर कृष्णजी से कहाः
अर्जुन उवाच
दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ (1.28)
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ॥ (1.29)
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते ।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ (1.30)
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ (1.31)
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ।
किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ (1.32)
येषामर्थे काङक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥(1.33)
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ (1.34)
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ (1.35)
निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।
पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ॥ (1.36)
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ (1.37)
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ (1.38)
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ (1.39)
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ (1.40)
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥(1.41)
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ (1.42)
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ (1.43)
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ (1.44)
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ (1.45)
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ (1.46)
(गीता - अध्याय » 1; श्लोक » 28-46)
अर्जुन बोले- हे कृष्ण! युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कम्प एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव! मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद! हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्यागकर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन! मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? हे जनार्दन! धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन! कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर सम्पूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण! पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय! स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिण्ड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चितकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा! शोक! हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।
अर्जुन के इन शुद्ध और सूक्ष्म विचारों को सुनकर कृष्णजी ने आश्चर्य से पूछा:
श्रीकृष्ण उवाच
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ (2.2)
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ (2.3)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 2-3)
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन! तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन! नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा॥3॥
इस पर अर्जुन ने कहा:
अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥(2.4)
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- ञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥ (2.5)
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो- यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥(2.6)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 4-6)
अर्जुन बोले- हे मधुसूदन! मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूँगा? क्योंकि हे अरिसूदन! वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूँगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना- इन दोनों में से कौन-सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं।
अर्जुन की वाणी से स्पष्ट है कि यह एक गृहयुद्ध था, जिसमें एक परिवार के दो पक्ष राज्यसत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सर्वनाश करना चाहते थे। अर्जुन के हृदय ने उन्हें इस भ्रातृहत्या और लोभ के लिए फटकार लगाई और अंतरात्मा की इस फटकार से प्रेरित होकर, वह एक महान सैनिक के रूप में युद्ध से घृणा करने लगे। लेकिन कृष्णजी ने उनके विचारों का खंडन किया और उन के सामने एक आधुनिक दर्शन प्रस्तुत किया जिसे गीता के कथावाचक ने इन शब्दों में उद्धृत किया है:
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ (2.11)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 11)
श्रीकृष्ण बोले, हे अर्जुन! तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पण्डितों के से वचनों को कहता है, परन्तु जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पण्डितजन शोक नहीं करते।
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ (2.12)
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ (2.13)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 12-13)
न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता।
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥2.18॥
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ (2.19)
न जायते म्रियते वा कदाचि-न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो-न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (2.20)
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ (2.21)
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (2.22)
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ (2.23)
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ (2.24)
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि॥ (2.25)
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ (2.26)
जातस्त हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ (2.27)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 18-27)
इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन! जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन! इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है अर्थात् तुझे शोक करना उचित नहीं है। किन्तु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो! तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है।
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ (2.30)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 30)
कृष्णजी ने एक और तत्त्वज्ञान की व्याख्या की, जिसकी वाणी उन्हीं के शब्दों में उद्धृत है:
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥
(गीता - अध्याय » 4; श्लोक » 36-37)
यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह सम्पूर्ण पाप-समुद्र से भलीभाँति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है।
योगसन्नयस्तकर्माणं ज्ञानसञ्न्निसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥ (4.41)
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ (4.42)
(गीता - अध्याय » 4; श्लोक » 41-42)
हे धनंजय! जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अन्तःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बाँधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन! तू हृदय में स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशय का विवेकज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ (5.7)
(गीता - अध्याय » 5; श्लोक » 7)
जिसका मन अपने वश में है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरण वाला है और सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ (5.10)
(गीता - अध्याय » 5; श्लोक » 10)
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भाँति पाप से लिप्त नहीं होता।
गीता के दर्शन पर एक दृष्टि
कृष्णजी के इस उपदेश का सार स्पष्ट शब्दों में यह है:
(1) चूँकि पुनर्जन्म की मान्यता के अनुसार व्यक्ति का बार-बार जन्म होता है, इसलिए उसे मारना कोई बुरी बात नहीं है। मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होगा और उसकी अमर आत्मा पर वध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(2) आत्मा के लिए शरीर की वही स्थिति है जो शरीर के लिए वस्त्र की है। तो अपने शरीर और आत्मा के संबंध को तोड़ना अपने पुराने कपड़ों को फाड़ने जैसा है। इस क्रिया को हत्या और उसके परिणाम को मृत्यु समझना, फिर उसे पाप और अपराध समझकर पछताना, अज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि में तो जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है वह वास्तव में उसकी हत्या नहीं करता, केवल उसकी आत्मा पर से शरीर का आवरण उतार देता है और यह कोई दुख की बात नहीं है। दुख की बात तो तब होती जब हत्या से आत्मा की भी मृत्यु हो जाती।
(3) जिसका अस्तित्व है उसका नष्ट होना निश्चित है। फिर जब मनुष्य को एक दिन मरना ही है तो उसे मारने में क्या बुराई है? जो अटल है सो होकर रहेगा, चाहे हमारे हाथ से हो या प्रकृति के हाथ से। प्रकृति तो उसे कल मारने ही वाली है, फिर अगर आज हम उसे मार दें, तो इसमें क्या बुराई है?
(4) जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए भलाई और बुराई का बंधन नहीं रह जाता, उसके लिए सभी कर्म वैध हो जाते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का भेद केवल उनके लिए है जो ज्ञानी नहीं हैं, बस ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आपके लिए बुरे से बुरा कर्म भी अपराध नहीं है।
इस शिक्षा का स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में मानव जीवन का कोई भी मूल्य न रहे। जिसका जी चाहे अपने दूसरे भाई के शरीर को एक पुराने कपड़े की तरह फाड़ दे और जब पूछताछ हो तो शरीर की नश्वरता और आत्मा के शाश्वत जीवन का दर्शन प्रस्तुत करके हत्या के आरोप से बरी हो जाए। फिर जो व्यक्ति ज्ञानी होने का दावा करता हो, उसके लिए तो हत्या ही क्या, कोई भी अपराध अपराध नहीं है और कोई पाप पाप नहीं है। वह आज़ादी के साथ हर तरह के अपराध करने के बाद भी निर्दोष रहता है।
एक ओर ते गीता ऐसी स्वच्छंदता के साथ युद्ध करने को प्रेरित करती है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपने पूरे 18 अध्यायों में उसने एक जगह भी यह नहीं बताया कि इस हिंसा और रक्तपात का उद्देश्य क्या है? किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह मानवजाति का ख़ून बहाना या आत्मा और शरीर के संबंध को विच्छेद करना वैध समझती है। युद्ध के विषय में युद्ध के उद्देश्य का प्रश्न वास्तव में एक मौलिक प्रश्न है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इस विध्वंसक काम को पवित्र बना सकती है, तो वह उद्देश्य की शुद्धता ही है। अन्यथा, अवैध उद्देश्यों के लिए युद्ध चाहे कितनी ही शालीनता से किया जाए, वह अवैध ही होगा और नैतिक क़ानून की दृष्टि में क्रूरता और पशुता के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन ‘गीता’ में इस मूलभूत प्रश्न की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और इस दिशा में मनुष्य का मार्गदर्शन करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
फिर भी, कुछ श्लोकों की अभिव्यक्ति को देखते हुए, कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध के उद्देश्य के बारे में गीता का क्या दृष्टिकोण है। एक स्थान पर कृष्णजी कहते हैं:
यदृच्छया चोपपन्नां स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ (2.32)
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ (2.33)
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्ति-र्मरणादतिरिच्यते ॥ (2.34)
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ (2.35)
अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ (2.36)
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ (2.37)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 31-37)
हे पार्थ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा । तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुःख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन! तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ (2.31)
(गीता - अध्याय » 2; श्लोक » 31)
तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है अर्थात् तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है।
गीता में केवल (2.31) ही एक ऐसा श्लोक मिलता है जो युद्ध के बेहतर नैतिक उद्देश्य की ओर इशारा करता है, लेकिन यह दुख की बात है कि गीता में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गयी है कि “धर्मयुक्त युद्ध” से उसका आशय क्या है। अगर “धर्मयुक्त युद्ध” का अर्थ केवल यह है कि अगर एक परिवार की दो शाखाएँ सिंहासन का दावा करती हों, और राजतंत्र के संविधान के अनुसार एक शाखा को शासन करने का अधिकार प्राप्त हो, तो उसे भ्रातृहत्या के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और युद्ध करके सिंहासन प्राप्त कर लेना चाहिए। “धर्मयुक्त युद्ध” अगर यही है, तो इस वाक्यांश की संपूर्ण नैतिकता समाप्त हो जाती है। ऐसे “धर्मयुक्त युद्ध” तो राजघरानों में सदा ही होते रहे हैं और किसी समझदार व्यक्ति ने कबी यह नहीं सोचा कि राजगद्दी के लिए अपने ही भाइयों और सगे संवंधियों से युद्ध करना और अपने राज-स्वार्थ के लिए अन्य सहस्रों मनुष्यों के प्राणों की बलि चढ़ा देना कोई भला और पवित्र काम है।
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धोलोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ (11.32)
तस्मात्त्वमुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ (11.33)
(गीता - अध्याय » 11; श्लोक » 32-33)
श्री कृष्ण बोले- मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ! यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन-धान्य से सम्पन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन! (बाएँ हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम ‘सव्यसाची’ हुआ था) तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा।
ये विचार उन आम विचारों से अलग नहीं हैं जो युद्ध से पूर्व हमेशा सैनिकों को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। न ही युद्ध के ये उद्देश्य उन उद्देश्यों से ऊंचे हैं जिनके लिए दुनिया के लोग अपने ही जैसे मनुष्यों का ख़ून बहाते हैं। वही धन और लोकप्रियता की चाह, वही सत्ता और साम्राज्य की चाह, वही हार का अपमान और बदनामी का डर, यहाँ भी युद्ध को प्रेरित कर रहा है, जो आम सांसारिक लोगों में युद्ध का उत्साह और हत्या की इच्छा पैदा करता है। इसमें कोई उच्च शिक्षा नहीं है, कोई उच्च नैतिक मार्गदर्शन नहीं है, कोई बेहतर आदर्श नहीं है। पाश्विक इच्छाओं और भावनाओं से श्रेष्ठ किसी इच्छा की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं किया गया है।
महर्षि मनु के युद्ध के नियम
महर्षि मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धार्मिक क़ानूनों का सबसे अच्छा संग्रह है। इसके उपदेश लगभग 1400 वर्षों से हिंदू राष्ट्रों और राज्यों में आदर्श रहे हैं। इसके लेखक का व्यक्तित्व काफ़ी हद तक अंधेरे में है, इसके लेखन का काल भी निर्धारित नहीं है। लेकिन यह तथ्य निश्चित है कि यह आर्यों के उस काल का ग्रन्थ है जब इसकी सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी थी और राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियमित संविधानों की ज़रूरत पैदा हो गई थी। इस प्रयोजन के लिए मनुस्मृति के अलावा और भी बहुत से शास्त्र और स्मृतियां लिखी गईं, लेकिन मनुस्मृति को उन सब पर प्राथमिकता प्राप्त है, क्योंकि अन्य पुस्तकें या तो मनुस्मृति के आधार पर तैयार की गई हैं या मनुस्मृति के विरुद्ध होने के कारण विद्वानों ने उन्हें नकार दिया है। धार्मिक पुस्तकों में आम तौर पर यह विचार व्यक्त किया जाता है कि जो कुछ “मनु कहते हैं वही सही है” और “मनुस्मृति के ख़िलाफ़ जो भी है वह मान्य नहीं है।” इसलिए हमारे पास हिंदू धर्म के क़ानूनों को जानने का इससे अच्छा कोई स्रोत नहीं है।
युद्ध का उद्देश्य
पहला प्रश्न युद्ध के उद्देश्य का है। महर्षि मनु ने इस पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन निम्नलिखित कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे किन उद्देश्यों के लिए युद्ध को अनुज्ञेय मानते हैं:
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ।। (7/89)
(मनुस्मृति - अध्याय » 7; श्लोक » 89)
जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामथ्र्य हो बिना डरे, पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं और मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं।
नित्यं उद्यतदण्डस्य कृत्स्नं उद्विजते जगत् ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ।। (7/103)
(मनुस्मृति - अध्याय » 7; श्लोक » 103)
जिस राजा की सेनाएं सर्वदा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं तो उससे सारा जगत् भयभीत रहता है इसीलिए सब प्राणियों को दण्ड से साधे अर्थात् दण्ड के भय से अनुशासन में रखे ।
सामादीनां उपायानां चतुर्णां अपि पण्डिताः ।
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ।। (7/109)
इस तरह विजय की तैयारी करने के बाद अपने सभी विरोधियों को या तो संधि कर के अपना आज्ञाकारी बना ले। (अगर वे स्वेच्छा से आज्ञाकारिता स्वीकार न करें तो) दूसरे माध्यम अपनाए। अर्थात् रिशवत, जोड़-तोड़ और युद्ध ।
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः ।
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत् ।। (9/251)
राजा इस विधि से धर्मयुक्त, सब कर्मों को भली भांति करता हुआ उन देशों को विजय करने की चेष्टा करे जो जीते नहीं गये हैं और फिर जीते हुये प्रदेशों की रक्षा करने की चेष्टा करे।
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः ।
शस्त्रेण वैश्यान्रक्षित्वा धर्म्यं आहारयेद्बलिम् ।। (10/119)
शस्त्र द्वारा विजय करना युद्ध से परांग मुख न होना, यह दोनों कार्य राजा के धर्म हैं और शास्त्रों से वैश्यों की रक्षा करके उनसे धर्मानुसार कर लेवें।
इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य के प्रश्न में महर्षि मनु के विचार भी श्रीकृष्ण के विचारों से बहुत भिन्न नहीं है। साम्राज्य विस्तार, राज्यों का अधिग्रहण, पड़ोसी देशों और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों का अपमान, जैसी विशुद्ध सांसारिक इच्छा से अधिक इनमें कोई नैतिक आदर्श नहीं दिखाई देता। महर्षि मनु भी सामान्य दुनियादार लोगों की भाँति शासन और राजसत्ता को शक्तिशाली लोगों का परम लक्ष्य मानते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी शक्ति साम्राज्य विस्तार के इस काम में निरन्तर लगाते रहें। बल प्रयोग की यह अवधारणा किसी नैतिक आदर्श का परिणाम नहीं हो सकती। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्यों का जीवन, राष्ट्रों की स्वतंत्रता और देशों की शांति राजाओं के साम्राज्य विस्तार के लोभ से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। किसी के लोभ की पूर्ति कभी नैतिकता को वांछित नहीं हो सकती। नैतिकता मानव जाति के समग्र सुधार और कल्याण की कामना करती है और युद्ध जैसे घातक कृत्यों की अनुमति केवल तभी देती है जब वह मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को दुष्ट शक्तियों द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए अनिवार्य हो जाए। महर्षि मनु या किसी अन्य हिन्दू दार्शनिक और विधिवेत्ता के दर्शन में युद्ध का यह उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता। जिन विद्वानों ने इसके विरुद्ध विचार व्यक्त किए वे अहिंसा के सिद्धांत तक पहुंच गए, जो मनुष्य के समग्र कल्याण के लिए रक्तपात की खुली अनुमति से कम घातक नहीं है। रक्तपात की खुली अनुमति हो या अहिंसा, वास्तव में दोनों का परिणाम एक ही है, अर्थात् राष्ट्रों और देशों का विनाश और दुष्ट और भ्रष्ट लोगों का वर्चस्व और प्रभुत्व।
युद्ध की नैतिक सीमाएँ
महर्षि मनु ने युद्ध के व्यावहारिक पहलू में बहुत कुछ विकसित किया और युद्ध की कार्रवाइयों को एक नियम के अधीन लाने के लिए ऐसी सीमाएं निर्धारित कीं हैं, जो कुछ हद तक इस्लाम द्वारा निर्धारित सीमाओं के समान हैं। नीचे हम उनके आदेशों को शब्दशः उद्धृत करते हैं:
न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून् ।
न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजनैः ।। (7/90)
राजा का धर्म है कि वह युद्ध करता हुआ युद्ध में शत्रुओं को न कूट शास्त्रों से, न निकलने में कठिन कर्णि शस्त्रास्त्रों से, और न प्रदीप्ताग्नियुक्त तेज शस्त्रास्त्रों से मारे।
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम् ।
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ।। (7/91)
न सुप्तं न विसंनाहं न नग्नं न निरायुधम् ।
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ।। (7/92)
न (गाड़ी या घोड़े पर सवार) पैदल को मारे, न स्त्री को, न हाथ जोड़े हुए क्षमायाची को, न जिसके सिर के बाल खुल गये हों। अत्यन्त घायल न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरूष को सत्पुरूषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धालोग कभी मारें । विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री, बालक वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरूषों पर शस्त्र कभी न चलावे । इसी प्रकार, न इधर उधर किसी स्थल में खड़े हुए, न नपुंसक, इसी प्रकार, न सोए हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नंगे, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुए को देखने वाले युद्ध-दर्शक, और न शत्रु के किसी पुरुष के साथ आए हुए को कभी युद्ध में मारे।
नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरिक्षतम् ।
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्मं अनुस्मरन् ।। (7/93)
छिन्न अस्त्र वाला, पुत्रादि की मृत्यु के कारण शोकार्त, कठिन घाव लगा हो, भयातुर, युद्ध से प्ररामुख (भागा हुआ) इन सब को सज्जनों के धर्म को विचार कर न मारें। इसी प्रकार, न आयुध-प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए, और न पलायन करते हुए शत्रु पुरुष को, सत्यपुरुषों के धर्म को स्मरण करके, कभी युद्ध में मारे।
रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्त्रियः ।
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ।। (7/96)
रथ, घोड़ा, हाथी, छतरी, धन, धान्य, पशु, स्त्री तथा सारा द्रव्य सोना, चाँदी के अतिरिक्त सीसा, पीतल आदि इन सबको जो जीतता है वही उसका स्वामी है। इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि लड़ाई में जिस घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेज आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका स्वामी है।
राज्ञश्च दद्युरुद्धारं इत्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यं अपृथग्जितम् ।। (7/97)
सोना, चाँदी, भूमि आदि जो उत्तम वस्तुयें जीत में प्राप्त हों उनका पाने वाला अपने राजा को देवे, यही वेद में लिखा है, तथा राजा उस वस्तु को उन सब शूरों को बाँट दे जिन्होंने देश विजय किया है।
उपरुध्यारिं आसीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ।। (7/195)
शत्रु दुर्ग में रहे वा बाहर रहे तथा युद्ध भी न करता हो परन्तु उसे घेरे रहे और उसके राज्य को पीड़ा पहुँचावे, घास, लकड़ी व जल इनमें व्यर्थ पदार्थों को डाल कर नष्ट करें। किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेरकर रोक रखे और इसके राज्य को पीडि़त कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित कर दे ।
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।
समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ।। (7/196)
ताल, दुर्ग प्राकार, परिखा (खाई), इन सब को नष्ट भृष्ट कर दें तथा निर्भयशत्रु को भयभीत करें और बरछी लेकर रात्रि को डहका नाम बाजे के शब्द से अति दुःख दें।
जित्वा संपूजयेद्देवान्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान् ।
प्रदद्यात्परिहारार्थं ख्यापयेदभयानि च ।। (7/201)
जब वह विजय प्राप्त कर ले, तो उसे विधिवत देवताओं की पूजा करनी चाहिए और धर्मी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, उसे छूट देनी चाहिए, और उसे सुरक्षा के वचनों की घोषणा करनी चाहिए।
सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम् ।
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ।। (7/202)
सब की सम्मति पाकर उस राजा के वश में जो हो उसको उसी के स्थान पर राजा बनावें, तथा उस राजा व उसके मन्त्रियों को वह उपदेश कर दें कि तुम ऐसा करना ऐसा न करना।
प्रो. हॉपकिंस लिखते हैं:
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मनु और विष्णु दोनों कहते हैं कि जब कोई राजा किसी बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, तो वह स्वयं उस देश के राजकुमार (अपने देश के नहीं) को वहां का राजा बना दे। उसे अपने शत्रु के राजपरिवार को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यह उस स्थिति में वैध है, जब वह राजपरिवार नीच जाति का हो। (कैम्ब्रिज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खंड 1, पृ. 290)
प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अन्य विशेषज्ञ, प्रोफेसर हवेल, जो हिंदू सभ्यता के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अपने इतिहास में लिखते हैं: विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच और आर्यों और ग़ैर-आर्यों (दास और दस्यु) के बीच युद्ध अक्सर होते थे, लेकिन चूंकि अंतर-आर्यन युद्ध में यह एक निश्चित नियम था कि युद्ध केवल राज्य के विस्तार के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। और यह कि एक पराजित आर्य राजा को अपदस्थ नहीं किया जाए, बल्कि विजयी राजा को चाहिए कि वह उसे अपना अधीनस्त और करदाता बना ले। इसलिए आपसी संघर्षों ने आर्यों की सामूहिक व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया। (History of Aryan Rule in India, P-33-34)
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् ।
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ।। (7/203)
उसे (निवासियों) के वैध (रीति-रिवाजों) को आधिकारिक बनाने दें, जैसा कि कहा गया है (होना), और उसे (नए राजा) और उसके मुख्य सेवकों को क़ीमती उपहारों से सम्मानित करने दें।
इनमें से कुछ आदेश ऐसी हैं जिनका युद्ध में पालन करना बिल्कुल असंभव है। उदाहरण के लिए, कि सवार पैदल की हत्या न करे, अगर शत्रु के बाल खुल जाएं तो उस पर हमला न करे, शत्रु के पास कवच न हो तो उसे छोड़ दिया जाए, नग्न, निहत्थे, उदास या आतंकित की हत्या न की जाए, अगर शत्रु किसी अन्य व्यक्ति से लड़ने में लगा हो, तो उसे न मारा जाए। इस प्रकार के आदेशों में सुधार की भावना पर दिखावे की नैतिकता प्रभावी हो गई है, इसलिए युद्ध की ज़रूरतों और नैतिक सीमाओं के बीच संतुलन नहीं रह पाया है। स्पष्ट है कि जब युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध होता है तो सैनिक इन बातों को ध्यान में नहीं रख पाता और अगर इनपर ध्यान देता है तो युद्ध नहीं कर सकता। दूसरी ओर, कुछ आदेशों में महर्षि मनु ने युद्ध की ज़रूरतों के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का त्याग कर दिया है। उदाहरण के लिए, शत्रु के सभी संसाधनों को नष्ट करके पूरे देश को भूखा रखने का आदेश किसी रूप में भी उच्च नैतिक संवेदनाओं के अनुरूप नहीं है। फिर भी कुल मिलाकर महर्षि मनु के ये आदेश बहुत ही सभ्य हैं। ये एक ऐसी प्रशिक्षित नैतिक चेतना को प्रकट करते हैं जिसमें शत्रुता और युद्ध की स्थिति में भी योद्धाओं के मानवीय दायित्वों का बोध है। यह उस उच्च नैतिक कल्पना तक पहुँच गया है कि मनुष्य पर उसके शत्रु के भी कुछ अधिकार हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस मामले में महर्षि मनु के नियम सैद्धांतिक रूप से इस्लाम के क़रीब हैं, हालांकि इतने संतुलित और विकसित नहीं हैं।
विजित राष्ट्रों के साथ व्यवहार
यह ऊपर कहा जा चुका है कि महर्षि मनु का क़ानून ऐसे समय में लिखा गया था जब ग़ैर-आर्य जातियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई थी और भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं बचा था, जिसके साथ आर्यों का युद्ध होता। इसलिए, मनु के धर्मशास्त्र में आर्य और ग़ैर-आर्य जातियों के बीच युद्ध के लिए निर्धारित क़ानूनों की तलाश करना व्यर्थ है। उस अवधि में, सभी ग़ैर-आर्य जातियां, जिनका वेदों में दास, दस्यु, राक्षस और असुर के रूप में उल्लेख किया गया है, या तो बस्तियों को छोड़कर पहाड़ों में शरण ले चुकी थीं या पराजित होकर आबादी का हिस्सा बन गयी थीं और सामूहिक रूप से उन्हें “शूद्र” नाम दिया गया था। तो मनुस्मृति से हम केवल यह जान सकते हैं कि विजयी हिंदू को परस्पर युद्ध में हारे हुए हिंदू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। युद्ध पर उनके आदेश हमें यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों को विजित ग़ैर-आर्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसे जानने के लिए हमें शूद्रों के बारे में मनु के आदेशों को देखना चाहिए:
(1) महर्षि मनु शूद्रों को स्वभाव से नीच ठहराते हैं। वे उन्हें कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निम्नतम प्राणी मानते हैं:
लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः ।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ।। (1/31)
लेकिन दुनिया की समृद्धि के लिए उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने मुंह, अपनी बाहों, अपनी जांघों और अपने पैरों से आगे बढ़ाया।
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ।। (2/31)
शर्मवद् ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षासमन्वितम् ।
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥ (2/32)
एक ब्राह्मण के नाम का (पहला भाग) शुभ, एक क्षत्रिय का शक्ति से जुड़ा होना चाहिए, और एक वैश्य का धन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन एक शूद्र का (कुछ व्यक्त करना) तिरस्कारपूर्ण है। (दूसरा भाग) एक ब्राह्मण (नाम) होगा (एक शब्द) ख़ुशी का अर्थ, एक क्षत्रिय का (एक शब्द) जिसका अर्थ है सुरक्षा, एक वैश्य का (एक शब्द) संपन्न होने का अभिव्यंजक, और एक शूद्र का (एक अभिव्यक्ति) निरूपित करना सेवा। ‘‘जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्णु वर्मा, वैश्य का विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये । जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त धर ले ।
सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किं चिज्जगतीगतम् ।
श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ।। (1/100)
जो कुछ इस संसार में है यह सब ब्राह्मण के हेतु है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञानबल से उनका ठीक ठीक लाभ भोग सकता है और दूसरे वर्ण ज्ञान की न्यूनता के कारण लाभ नहीं भोग सकते। इस हेतु सब कुछ ब्राह्मण ही का है, क्योंकि वह ब्रह्माजी के उपदेश से सबको धर्म की शिक्षा देने (सिखलाने) के हेतु उत्पन्न हुआ है। अतएव सबसे श्रेष्ठ हैं।:
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ।। (10/4)
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीनों वर्ण द्विजन्मा कहलाते हैं और चैथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है। अन्य पाँचवाँ वर्ण नहीं है।ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन द्विज कहलाते हैं। चैथी एक जाति शूद्र है। पंचम जाति कोई नहीं है।
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ।। (12/43)
हाथी, घोड़ा, सुअर, म्लेच्छ, सिंह, बाघ, शूद्र इन सब गतों को तामसी। म्लेच्छ उसे कहते हैं जो निकृष्ट पदार्थों का इच्छुक हो व मांस, मदिरा, व्यभिचार का इच्छुक हो। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने हारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ।
(2) मनु शूद्रों को जन्मजात अपवित्र और कमीना मानते हैं और समाज में द्वेज, अर्थात् कुलीन आर्य जातियों को, उनसे पूरी तरह बचने का आदेश देते हैं।
शूद्रां शयनं आरोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ।। (3/17)
शूद्र कन्या को अपने पलंग पर बिठाने से ब्राह्मण अधोगति पाता है।
न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः ।
न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ।। (4/79)
दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चाण्डाल, पुल्कस, धनगर्वित, मूर्ख धोबी, आदि तथा अन्त्यावसायी हों उनके संसर्ग (साथ) में एक वृक्ष की छाया में न रहें। पतितों के साथ न रहें। न चांडालों के साथ। न पुल्कस अर्थात् कुलटा स्त्री की सन्तान के साथ। न मूर्खों के साथ। न घमण्डियों के साथ। न अत्यन्त नीचों के साथ। न उनके साथ जो नीचों के साथ रहने में रुचि रखते हैं।
(शूद्र पुरुष के वीर्य और ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा व्यक्ति “चांडाल” होता है।(मनु,10:12)
यो ह्यस्य धर्मं आचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम् ।
सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति ।। (4/81)
जो पुरुष शूद्र को धर्म तथा व्रतोपदेश करता है वह उस शूद्र सहित असंवृत नाम नरक को प्राप्त होता है।
नाविस्पष्टं अधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ।। (4/99)
पाठ में स्पष्ट शब्द और स्वर सहित पढ़ें, शूद्र के समीप पाठ न करें और यदि रात्रि के चौथे पहर में वेदपाठ से श्रमित हो जाये तो सोवे नहीं।
“अगर एक शूद्र जानबूझ कर वेद के शब्दों को सुन ले, तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला दिया जाए। और अगर वह वेद के श्लोक पढ़े, तो उसकी जिभा काट ली जाए और अगर वह उसे याद करे तो उसके शरीर को टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाए।” (गौतम, 12:4-6)
अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च ।
शुक्तं पर्युषितं चैव शूद्रस्योच्छिष्टं एव च ।। (4/211)
दोषी व दुष्ट प्रकृति, पंढ (हिजड़ा), दम्भी आदि का अन्न, बासी अन्न (अर्थात् वह अन्न जो बिना-खटाई मिश्रित किये खट्टा हो जावे), तथा शूद्र का जूठा अन्न इन सबको भोजन न करें। पपी का, हिजड़े का, व्यभिचारिणी स्त्री का, दंभी का, खमीर उठा हुआ, बासी, तथा शूद्र का जूठा।
“एक शूद्र द्वारा तैयार किया गया भोजन, चाहे उसने उसे छुआ हो या नहीं, खाने की अनुमति नहीं है।” (स्मिथ, 1:5:22:16)
अगर एक ब्राह्मण ऐसी स्थिति में मर जाता है कि उसके पेट में शूद्र का खाना मौजूद हो, तो अगले जन्म में वह गाँव के सूअर के रूप में जन्म लेगा, (विशिष्ठ, 6:27)
राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ।। (4/218)
एक राजा का भोजन उसकी शक्ति को कम करता है, एक शूद्र का भोजन उसकी पवित्र विद्या को, एक सुनार का भोजन उसकी लंबी उम्र, एक चर्मकार का भोजन उसकी प्रसिद्धि;
1-राजा, 2-शूद्र, 3-सोनार, 4-चमार, इन लोगों का अन्न यथा क्रम 1-तेज, 2-ब्रह्मतेज, 3-आयु, 4-यश का नाश करता है।
नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः ।
आददीतामं एवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ।। (4/223)
विद्वान् ब्राह्मणों को शूद्र का बनाया हुआ भोजन न खाना चाहिये, यदि घर में अन्न न हो तो एक रात्रि के भोजन भर कच्चा अन्न ले लेने में कोई दोष नहीं है।
दिवाकीर्तिं उदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।
शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति ।। (5/85)
चाण्डाल, मासिक धर्म वाली स्त्री, जिसने बेटा या बेटी जनी हो, मृतक के छूने वाले, इन सबको छूकर स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं।
दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।
पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ।। (5/92)
नगर के 1-पश्चिम, 2-उत्तर, 3-पूर्व, 4-दक्खिन द्वार से (यथाक्रम( प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ द्वार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का शव ले जाना चाहिये।
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् ।
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ।। (5/104)
एक मृत ब्राह्मण को शूद्र द्वारा ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वहां एक भी ब्राह्मण मौजूद न हो। शूद्र के स्पर्श से ब्राह्मण का अंतिम संस्कार अपवित्र हो जाता है, और वह स्वर्ग नहीं जा सकता है।
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।
वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ।। (10/12)
एक शूद्र पुरुष से वैश्य, क्षत्रिय, और ब्राह्मण महिलाओं के यहां जो संतान जन्म लेगी वह संकर होगी, वह क्रमश: आयोगव, क्षत्रिय, और चाण्डाल कही जाएगी। ये सबसे नीच जातियां हैं।
चण्डालश्वपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।
अपपात्राश्च कर्तव्या धनं एषां श्वगर्दभम् ।। (10/51)
वासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।
कार्ष्णायसं अलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः ।। (10/52)
न तैः समयं अन्विच्छेत्पुरुषो धर्मं आचरन् ।
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ।। (10/53)
अन्नं एषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ।। (10/54)
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः ।
अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ।। (10/55)
वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ।
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ।। (10/56)
चाण्डाल व स्ववच यह दोनों ग्राम के बाहर बसें। मृत पुरुषों के वस्त्र पहनें, अच्छे बरतन का प्रयोग न करें, टूटे फूटे बरतनों में भोजन करें। उनकी सम्पत्ति केवल कुत्ते और गधे हों। लोहे के आभूषण पहनें और सदैव घूमते रहें । धर्मात्मा पुरुष इन लोगों के साथ दर्शन आदि व्यवहार न करें इनके विवाह परस्पर ही होते रहें और व्यवहार भी अपने ही में करें। उनका भोजन दूसरों के अधीन है। फूटे बरतन में अन्न देना चाहिये और देने वाला उनके हाथ में न थमाए। ये लोग रात्रि में गाँव व नगर में घूमने न पावें। यह लोग दिन में कार्यार्थ आवें तो राजा द्वारा निर्धारित जाति चिन्ह उनके शरीर पर लगे हों। जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उसको ले जाने का काम करें, यह शास्त्र का नियम है। चाण्डाल राजा की आज्ञा से शास्त्र विधि के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों का वध करें और वे ही बध्य (मकतूल) पुरुषों के वस्त्र, शय्या, आभूषणों ले लेवें।
न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हि चित् ।
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ।। (11/24)
ब्राह्मण यथार्थ शूद्र में कभी धन याचना न करें यदि धन याचना कर उस धन से यज्ञ करे तो दूसरे जन्म में चाण्डाल होता है।
चरितव्यं अतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।
निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ।। (11/53)
अतएव सदा पाप से मुक्त होने के हेतु प्रायश्चित और उत्तम कर्म करना चाहिये और जो लोग प्रायश्चित नहीं करते वे घृणित लक्षणों युक्त होते हैं।
अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टं एव च ।
जग्ध्वा मांसं अभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ।। (11/152)
अगर कोई ब्राह्मण शूद्र या स्त्री का उच्छिष्ट (जूठन) अन्न, या ऐसा अन्न जिसे खाना उचित नहीं है, खा ले, या मांस, जो सर्वथा अभक्ष्य है, खा ले, तो एक सप्ताह तक जौ के सत्तू के अतिरिक्त कुछ न खाए।
(3) मनु शूद्रों को द्वेजों की ग़ुलामी करने पर मजबूर करते हैं। उनके अनुसार शूद्र का जन्मजात और स्वाभाविक दायित्व ही यह है कि वह द्वेजों की सेवा करे।
एकं एव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।
एतेषां एव वर्णानां शुश्रूषां अनसूयया ।। (1/91)
शूद्र के लिये एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया है, अर्थात् तन और मन से निन्दा ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को छोड़ कर तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करना।
विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ।। (10/123)
ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का सबसे बढ़कर धर्म है और जो शूद्र इसको छोड़ कर दूसरा कार्य करता है वह अपने जीवन को निष्फल खोता है।
शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतं अक्रीतं एव वा ।
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ।। (8/413)
ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों के सेवार्थ ही बनाया है इस हेतु शूद्र चाहे मोल लिया हुआ हो चाहे वेतनभोगी हो या वेतनभोगी न हो उससे बराबर कार्य लेना चाहिये।
न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते ।
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ।। (8/414)
स्वामी यदि शुद्र को दासकर्म से मुक्त नहीं करता तो वह दास दासकर्म से मुक्त नहीं होता क्योंकि दासकर्म शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न है, इस संबंध को कौन छुड़ा सकता है।
(4) महर्षि मनु शूद्र को उसकी अपनी अर्जित संपत्ति पर भी मालिकाना अधिकार देने से इंकार करते हैं।
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद्द्रव्योपादानं आचरेत् ।
न हि तस्यास्ति किं चित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ।। (8/417)
ब्राह्मण दास (शूद्र) से धन ले लेवे, इनमें कुछ विचार न करें क्योंकि वह धन कुछ उसकी सम्पत्ति नहीं है, दास तो निर्धन है, वह जो धन एकत्र करे उस धन पर स्वामित्व उसके स्वामी का है।
वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।
तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतां इदं जगत् ।। (8/418)
वैश्य और शूद्र यह दोनों अपने कार्य से निष्कर्म न होने पावें यदि यह दोनों अपने धर्म से च्युत हों तो जगत् को क्षोभित (दुष्कर्मी) कर दें।
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।
शूद्रो हि धनं आसाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ।। (10/129)
शूद्र सामथ्र्य रखने पर भी धन संचय न करे क्योंकि शूद्र के पास धन हो जाने से वह ब्राह्मणों को हानि पहुँचाता है अर्थात् जब मूर्ख के पास धन होता है तो वह विद्वानों की सेवा परित्याग कर देता है और उन्हें तुच्छ समझने लगता है अतः धन से शूद्र का धर्म नाश हो जाता है।
(5)। उत्तराधिकार के क़ानून में भी महर्षि मनु ने द्वेजों और शूद्रों के बीच भेदभाव रखा है, कुछ मामलों में तो शूद्रों को उत्तराधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया है और कुछ मामलों में उन्हें द्वेजों की तुलना में निम्न दर्जा दिया गया है:
ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ।। (9/149)
कीनाशो गोवृषो यानं अलङ्कारश्च वेश्म च ।
विप्रस्याउद्धारिकं देयं एकांशश्च प्रधानतः ।। (9/150)
त्र्यंशं दायाद्धरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः ।
वैश्याजः सार्धं एवांशं अंशं शूद्रासुतो हरेत् ।। (9/151)
सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।
धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित् ।। (9/152)
चतुरोऽंशान्हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।
वैश्यापुत्रो हरेद्द्व्यंशं अंशं शूद्रासुतो हरेत् ।। (9/153)
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।
नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ।। (9/154)
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ।। (9/155)
समवर्णासु वा जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् ।
उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ।। (9/156)
क्रमानुसार चारों वर्ण की स्त्रियाँ जब ब्राह्मण के घर में हों और उन स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न हो उनके बीच विभाजन इस प्रकार होगा। किसान, नैकर, प्रत्येक द्रव्य तथा घोड़ा, साँड, रथ आदि सवारी, उत्तम आभूषण व वस्त्र में जो सर्वोत्तम हो उनमें से एक-एक वस्तु ब्राह्मणी के पुत्र को देकर शेष को निम्नलिखित विधि से विभक्त करें। ब्रह्माणी के पुत्र को तीन भाग, क्षत्राणी के पुत्र को दो भाग, वैश्य के पुत्र को डेढ़ भाग और शूद्रा के पुत्र को एक भाग मिलना चाहिये। अर्थात् 6-4-3-2 की निसवत् होनी चाहिये। अथवा जो विधि आगे कहेंगे उसके अनुसार धर्म ज्ञाता पुरुष सारी सम्पत्ति को दस भागों में विभाजित करके धर्मानुसार अंश विभाग करें। ब्रह्माजी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिय का पुत्र तीन भाग, वैश्य का पुत्र दो भाग और शूद्रा का एक भाग लेवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की स्त्रियों में ब्रह्मणी से पुत्र उत्पन्न हुआ हो परन्तु धर्मतः शूद्रा के पुत्र को दश मास से अधिक न देवें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के धन को शूद्रा का पुत्र नहीं ले सकता। उसका पिता जो कुछ देवे वही उसका धन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पुत्र जो समवर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुये हों। वह बड़े केा उद्वार नाम का स्वत्व देकर शेष को समान भागों में विभक्त कर लें।
(6)। आपराधिक क़ानूनों में, महर्षि मनु शूद्रों के साथ बहुत सख़्त हैं। वह उनके जीवन और सम्मान को क़ानून की सुरक्षा देने में बहुत कृपणता से काम लेते हैं, और इसके विपरीत, वे द्वेजों के अधिकारों को परिभाषित करने और उनकी रक्षा करने में इतनी उदारता दिखाते हैं कि शूद्रों का संवैधानिक अस्तित्व शून्य हो होकर रह जाता है:
एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ।। (8/270)
यदि शूद्र अर्थात् मूर्ख सेवक, विद्वान्, सैनिक (क्षत्रिय) व व्यापारी को अपशब्द कहे तो उसकी जीभ छेदन करने योग्य है, क्योंकि वह जिन लोगों की सेवा के हेतु नियत हुआ है उनकी सेवा के स्थान पर उनकी मानहानि (अपमान) करता है।
नामजातिग्रहं त्वेषां अभिद्रोहेण कुर्वतः ।
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः ।। (8/271)
धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणां अस्य कुर्वतः ।
तप्तं आसेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ।। (8/272)
जो शूद्र ‘अरे तू फलाने ब्राह्मण से नीच’ ऐसा अपशब्द ब्राह्मणों आदि द्विजातियों के नाम तथा जाति का सशब्द उच्चारण कर कहे, उसके मुँह में तप्त लोहे की दश अंगुल की कील ठोकनी चाहिये। जो अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश करे, राजा उसके मुख और कान में तप्त (गरम) तेल डलवावे।
सहासनं अभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।
कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ।। (8/281)
नीच पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करें तो उसकी कमर को चिन्हित कर दाग़ देकर निकाल दें अथवा इस प्रकार उसके चूतड़ को कुछ कटवाड़े जिससे चिन्ह तो बन जावे परन्तु मरने न पावे।
वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् ।
यो ब्राह्मण्यां अगुप्तायां तावुभौ दण्डं अर्हतः ।। (8/382)
पति आदि से सुरक्षित वैश्य की स्त्री से क्षत्रिय भोग करे व वैसी ही क्षत्राणी से वैश्य भोग करे तो जो दण्ड अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले को कहा है वही दण्ड देना।
अवनिष्ठीवतो दर्पाद्द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः ।
अवमूत्रयतो मेढ्रं अवशर्धयतो गुदम् ।। (8/282)
अहंकार से नीच पुरुष श्रेष्ठों के ऊपर थूके तो उसके दोनों ओंठ छेद डालें, मूत्र डाले तो लिंग (मूत्रेन्द्रिय) को काट डालें और ऊपर से अपना वायु (पाद) निकाले तो गुदा छेद डालें।
केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् ।
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ।। (8/283)
ब्राह्मण के बाल, पाँव, दाढ़ी, ग्रीवा (गर्दन) अंडकोष (फोतों) को पकड़ने वाले शूद्र के दोनों हाथों को कटवा दें। उसको कष्ट होने का विचार न करें।
शूद्रो गुप्तं अगुप्तं वा द्वैजातं वर्णं आवसन् ।
अगुप्तं अङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ।। (8/374)
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्री पति आदि से सुरक्षित हो वा न हो, उससे भोग करने वाले शूद्र की मूत्रेन्द्रिय काट लेनी व सारी सम्पत्ति हरण कर (छीन) लेनी चाहिये व प्राणदण्ड देना चाहिये परन्तु अरक्षित स्त्री से भोग करने में मूत्रेन्द्रिय छिन्न करना व सारी सम्पत्ति हरण कर लेना यही दण्ड देवें और सुरक्षित से भोग करने में उपरोक्त तीनों दण्ड देवें।
वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ।
सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ।। (8/375)
सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने में वैश्य को एक वर्ष पर्यन्त कारागार में रखना चाहिये, तत्पश्चात् सारी सम्पत्ति हरण कर लेनी चाहिये और उसी अपराध में क्षत्रिय को सहस्र पण दण्ड देवें तथा गधे के मूत्र से सिर मुँडवा देवें।
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।
वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ।। (8/376)
पति आदि से अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य को यथाक्रम पाँच सौ व सहस्र पण दंड देवें।
उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।
विप्लुतौ शूद्रवद्दण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना ।। (8/377)
पति आदि द्वारा सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य दोनों शूद्र के समान दण्डनीय हैं अर्थात् सब अंग छिन्न करने चाहिये, चाहे लाल कुश से ढक कर वैश्य को और सरहरी से ढककर क्षत्रिय को जलाना चाहिये वह दण्ड पतिव्रता व सद्गुणी स्त्री से भोग करने में जानना चाहिये।
सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाद्व्रजन् ।
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ।। (8/378)
पति आदि से सुरक्षित ब्राह्मणी से बलात्कार करने वाले ब्राह्मण को सहस्र पण दण्ड देना चाहिये। और उस ब्राह्मणी की इच्छा से भोग करने वाले ब्राह्मण को पाँच सौ पण दण्ड देना चाहिये।
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनं अक्षतम् ।। (8/380)
न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विद्यते भुवि ।
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ।। (8/381)
यदि ब्राह्मण (अर्थात् विद्वान पुरुष) बहुत पापों का अपराधी हो तो भी उसका वध न करें, वरन् शारीरिक दण्ड भी न देकर अपने राज्य से निकाल दें। संसार में विद्वान अर्थात् ब्राह्मण के वध से अधिक कोई पाप नहीं क्योंकि इससे अध्ययन-क्रम को हानि पहुँचती है। अतः राजा ब्राह्मण को वध करने का विचार मन में भी न लावे।
ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम् ।
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ।। (9/248)
जो क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र, ब्राह्मण को जान बूझकर हत्या करे उसकी विविध प्रकार के कष्ट जिनमें उद्विंगता व शोक संयुक्त हो राजा उसके द्वारा प्राणदण्ड देवे।
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।
वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ।। (11/127)
त्र्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम् ।
वसन्दूरतरे ग्रामाद्वृक्षमूलनिकेतनः ।। (11/128)
जब कोई ब्राह्मण अनिच्छा से व अज्ञानता से किसी क्षत्रिय का वध कर डाले तो एक सहस्र गाय और एक बैल प्रायश्चित्तार्थ दूसरे ब्राह्मण को दें। अथवा यथाविधि सिर पर जटा रखाये गाँव से बाहर अति दूर किसी वृक्ष की जड़ में निवास कर तीन वर्ष पर्यन्त ब्रह्महत्या वाले .प्रायश्चित को करें।
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याच्चैकशतं गवाम् ।। (11/129)
ब्राह्मण वैश्य की हत्या करके एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्महत्या के प्रायश्चित में व्यतीत करता हुआ व्रत करे अथवा एक सौ गऊ दान करे।
एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासाञ् शूद्रहा चरेत् ।
वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ।। (11/130)
मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकं एव च ।
श्वगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ।। (11/131)
पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत् ।
उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्तं वाब्दैवतं जपेत् ।। (11/132)
ब्राह्मण शूद्र के वध करने में छः मास पर्यन्त ब्रह्महत्या के प्रायश्चित को करे और खेत बैल और दस गऊ ब्राह्मण को देवे। यह भी अज्ञानता से वध करने में जानना। इन सब व्रतों के करने में कपाल ध्वजा को त्याग देना चाहिये। बिल्ली, नेवला, नीलकण्ठा, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ इनमें से किसी एक की हिंसा करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित करें अर्थात् हिंसा शूद्र की हत्या के समान समझें। अथवा तीन रात्रि दूध पीवें और यदि अशक्त हों तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चलें, यह भी न हो सके तो तीन रात्रि नदी में स्नान करें, यह भी न हो सके तो आपोहिष्ठा नाम वाले सूक्त का जप कर यह प्रायश्चित अज्ञानता से वध करने का है।
ये आदेश अपनी व्याख्या स्वयं कर रहे हैं, हिन्दू क़ानून पराजित समुदाय को जिस अपमान की दृष्टि से देखता है और समाज में उन्हें जो निम्नतर दर्जा देता है, वह इन आदेशों से स्पष्ट है। इसके विपरीत अगर हम इस्लाम के तहत ग़ैर-मुस्लिम ज़िम्मियों के अधिकारों को देखें, तो ज़मीन-आसमान का अंतर दिखाई देगा।
वंश-आघारित भेदभाव
हिन्दू समाज में जाति विभाजन “वर्ण” पर आधारित है। आरंभिक काल में जिन्हें दास और दस्यु की उपाधि दी जाती थी और बाद में जिन्हें शूद्र कहा गया, उनका यह अपमान उनके बुरे कर्मों के आधार पर नहीं था, बल्कि इस आधार पर था कि वे ग़ैर-आर्य मूल के थे। ऊपर उद्धृत उत्तराधिकार क़ानून, दंड विधान और सामाजिक क़ानूनों के नियमों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भलाई के काम करने वाले एक गुणी शूद्र को भी वे अधिकार नहीं दिए गए हैं, जो गंभीर अपराध करने वाले एक दुष्कर्मी ब्राह्मण को प्राप्त हैं। एक ब्राह्मण का पुत्र जो एक शूद्र महिला के गर्भ से पैदा होता है, चाहे वह कितना ही भला मनुष्य हो, उसे वे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जो ब्राह्मण महिला के गर्भ से जन्मे उसके अपने भाई को प्राप्त होते हैं। शूद्र पिता की संतान अगर ब्राह्मण माता से पैदा हुई हो, तो यह जन्म ही उसे चांडाल बना देता है और वह तिरस्कृत जीवन जीने को अभिशप्त हो जाता है, जो मनु ने चांडालों के लिए निर्धारित कर दिया है। हिन्दू धर्म ने प्रतिष्ठा और तिरस्कार को मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों से नहीं, बल्कि वीर्य और गर्भ से जोड़ रखा है। इस विषय में महर्षि मनु ने बहुत विस्तार से काम लिया है। वे कहते हैं:
जातो नार्यां अनार्यायां आर्यादार्यो भवेद्गुणैः ।
जातोऽप्यनार्यादार्यायां अनार्य इति निश्चयः ।। (10/67)
तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।
वैगुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ।। (10/68)
सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा ।
तथार्याज्जात आर्यायां सर्वं संस्कारं अर्हति ।। (10/69)
उत्तम बीज बोने से नीची योनि में उत्पन्न हुआ अर्थात् ब्राह्मण से शूद्रों में उत्पन्न हुआ यज्ञादि उत्तम कर्मों के करने से श्रेष्ठ हो सकता है और नीच बीज से ऊँची योनि में उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं। यह सिद्धान्त नहीं है कि दोनों संस्कार योग्य नहीं हैं क्योंकि प्रथम नीच जाति में उत्पन्न हुआ है और दूसरा प्रतिलोम है। जिस प्रकार उत्तम बीज उत्तम खेत पड़ने से उत्तम अन्य उपजता है उसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठ स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र सब संस्कारों के योग्य होता है।
अनार्यं आर्यकर्माणं आर्यं चानार्यकर्मिणम् ।
संप्रधार्याब्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ।। (10/73)
एक ग़ैर-आर्यन जो एक आर्यन की तरह कार्य करता है, और एक आर्यन जो एक ग़ैर-आर्यन की तरह कार्य करता है, पर विचार करने के बाद, निर्माता ने घोषणा की, 'वे दोनों न तो समान हैं और न ही असमान हैं।' अथात् न वे प्रतिषठा में समान हैं और न दुष्कर्म में असमान।
कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने यह साबित करने की कोशिश की है कि शूद्र वास्तव में ग़ैर-आर्यन मूल निवासी नहीं थे, बल्कि स्वयं आर्य जाति के निम्न वर्ग के लोग थे। लेकिन वास्विक शोध के आलोक में यह दावा स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूद्रों में आर्य मूल के वे लोग भी शामिल थे जिन्हें वर्ण आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में जाति से निष्कासित कर दिया जाता था। (Vedic index of names and subjects, Vol. ll,265,391) लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शूद्रों का वर्ग आम तौर पर ग़ैर-आर्य जातियों पर आधारित था, जिन्होंने अपना घर छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में निकल जाने के बजाय आर्य विजेताओं की ग़ुलामी में रहना स्वीकार कर लिया था। भाषाई और ऐतिहासिक शोधों से यह सिद्ध होता है कि शूद्र मूल रूप से एक प्राचीन भारतीय जनजाति का नाम था जिसे आर्यों ने सबसे पहले अटक नदी घाटी में पराजित किया था। उसके बाद आर्यों के शासन की अधीनता स्वीकार कर लेने वाली भारतीय जनजातियों को शूद्र और युद्ध करने वाली जनजातियों को दस्यु और मलेच्छ कहा जाने लगा। (Willson, Indian castes, Vol.l P.lll)
प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रमुख विद्वान इस मत की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, “Vedic India” के रचयिता Zenaide Alexeïevna Ragozin लिखते हैं :
“ This division is that into Aryas and Dasyus. Who the former are we know well, and a natural association leads us to the conclusion that the latter are no other than the native— or non-Aryan peoples whom the Aryan immigrants found in the land, and whom, after a long period of struggle, they reduced into more or less reluctant submission. There is no doubt but that we have here the first beginnings of caste, for this sweeping division is singularly like the modern one into "twice-born” and Shudra. Besides, the name for caste is even now varna, which means "color,” and we shall presently see that the difference of color between the white conquerors and the dark-skinned natives is continually alluded to by the Vcdic poets. Then, too, the word Dasyu, with the changes of meaning it has undergone, tells an eloquent tale. It is an old Aryan word, and the Persians continued to use it in its original harmless sense of peoples, nations. In Dareios historical rock inscriptions we find it so used, also in opposition to Aryas, to designate the populations of the provinces. In India it took a hostile shading — that of “enemies,” whence it easily passed into the cloudland of Vedic mythology, with the meaning of "fiends,” “evil demons," — the powers of darkness and drought — the “foes" whom Indra eternally combats and conquers with the help of the Maruts, the Angiras, and other beings of light. Logical and natural as the transition is, it adds very greatly to the difficulties of Vedic interpretation, because, when Indra or Agni are besought to drive away and annihilate the Dasyus, or are said to have destroyed the fastnesses of the Dasyus, it is frequently all but impossible to decide which “enemies” arc meant — the earthly or the mythical ones. The last change which the word underwent is very significant: it ended by meaning simply “slave, servant," (slightly altered into dasa) thus telling of conquest completed, and closely answering the more modem Shudra. We may, then, set down as correct the equation':
Arya — Dasyu= “twice-born” — Shudra.
And if any more proof be wanted of the fact that the servile class was made such by conquest, we have it in a passage of Manu's Code, which forbids the twice born to associate with a Shudra “even though he were a king." What can a Shudra king be but a native sovereign ?
It were impossible to exaggerate the loathing and contempt with which the Aryan regarded those whom they were robbing of land and liberty. These feelings primarily aroused by that most incradicable and unreasoning of human instincts, race antagonism, find vent in numberless passages of great value, because they enable us to piece together a tolerably correct picture of what those aborigines must have been, and in what manner they chiefly contrasted with their conquerors. The difference in color and cast of features is the first to strike us, and in that, as already hinted, we trace the beginnings of caste distinction. "Destroying the Dasyus, Indra protected the Aryan color," gratefully proclaims one poet. “Indra," says another, “protected in battle the Aryan worshipper, he subdued the lawless for Manu, he conquered the black skin." “He [Indra] beat the Dasyus as is his wont ... he conquered the land with his fair [or white] friends. . . ." Other names given by their Aryan conquerors are “goat-nosed" and “noseless” (anaso, evidently ail exaggeration of “flat-nosed"), while the Aryan gods are praised for their beautiful noses. The Dasyus are accused of having no sacred fires, of worshipping mad gods, of eating raw meat, and, lastly, it would appear that they were held to be dangerous sorcerers: “Thou [Indra] hast made the Disa's magic powerless against the Rishi.” Needless to add that difference of language completed the barrier which the victors later strove to render impassable.
Although the opposition of Arya to Dasyu or Dasa, of “twice-born” to Shudra, is a perfectly established and intelligible fact, it were a mistake to see in “ Dasyu " or “ Shudra " the names of a particular nation: they applied to all that were not Aryan, somewhat after the manner that, in classic antiquity, all went by the name of "Barbarians" who were not Greeks or Romans. (Zenaide A. Ragozin, Vedic India, Page 282-285)
“यह विभाजन आर्यों और दस्युओं के बीच है। पहले वाले कौन हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, रहे बाद वाले, तो प्राकृतिक जुड़ाव हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि वे मूल निवासी या ग़ैर-आर्य लोगों के अलावा कोई और नहीं हैं। ये वे लोग हैं, जिन्हें आर्य आप्रवासियों ने इस देश में पाया, और जिन्हें उन्होंने, एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग समर्पण की स्थिति में पहुंचा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, यहीं से जाति-विभाजन की शुरुआत होती है, क्योंकि यह व्यापक विभाजन आधुनिक विभाजन की तरह ही "द्वेज" और “शूद्र” है। इसके अलावा, जाति के लिए आर्यों की भाषा में ‘वर्ण’ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है "रंग”। वैदिक कवियों द्वारा गोरे विजेता और काले रंग के मूल निवासियों के बीच रंग के अंतर का लगातार उल्लेख किया गया है। फिर दस्यु शब्द, अपने अर्थों में परिवर्तन के साथ, एक स्पष्ट कहानी कहता है। यह एक पुराना आर्यन शब्द है, जिसे ईरानी लोग उसके मूल हानिरहित अर्थों (जाति और समुदाय) में, उपयोग करते थे। डेरियस के ऐतिहासिक शिलालेखों में हम पाते हैं कि इसका उपयोग आर्यों के विरोध में भी प्रांतों की आबादी को नामित करने के लिए किया गया था। भारत में इसने एक शत्रुतापूर्ण छायांकन ले लिया, वह "दुश्मनों" के अर्थ में बोला जाने लगा। यहाँ से यह वैदिक पौराणिक कथाओं में आसानी से समा गया और "असुर," "दुष्ट” “राक्षस," “भूत” “पिशाच” के अर्थों में बोला जाने लगा। इससे अंधेरे और अकाल की शक्तियोँ का अर्थ लिया जाने लगा - जिससे इंद्र मरुतों, अंगिरों और प्रकाश के अन्य प्राणियों की मदद से सदा लड़ता रहता है और जीतता है। यह जितना तार्किक और स्वाभाविक है, उतना ही यह वेदों की समझ और व्याख्या को कठिन बनाता है, क्योंकि, जब इंद्र या अग्नि से दस्युओं को भगाने और उनका सफ़ाया करने का अनुरोध किया जाता है, या कहा जाता है कि उन्होंने दस्युओं की शक्ति को नष्ट कर दिया है, तो यह तय करना अक्सर असंभव हो जाता है कि कौन से "दुश्मन" की बात हो रही है - सांसारिक या पौराणिक। इस शब्द में आख़िरी बदलाव महत्वपूर्ण है: यह केवल "सेवक" या “दास” के अर्थ में बोला जाने लगा और थोड़ा सा शाब्दिक परिवर्तन कर के ‘दस्यु’ को ‘दास’ बना दिया गया। इस प्रकार यह विजय पूर्ण होने की सूचना देता है, और अधिक आधुनिक शब्द “शूद्र” के निकट पहुंच जाता है। इस समीकरण के अनुसार:
आर्य - दस्यु = द्वेज - शूद्र।
यदि इस तथ्य का कोई और प्रमाण चाहिए कि शूद्रों को विजय द्वारा ग़ुलाम बनाया गया था, तो वह हमें मनुस्मृति में मिलता है, जिसमें द्वेज को शूद्र के साथ संपर्क रखने से हर हाल में मना किया गया है, चाहे वह शूद्र एक राजा ही क्यों न हो। एक शूद्र राजा एक देशी शासक के सिवा और क्या हो सकता है?
जिस घृणा और तिरस्कार के साथ आर्य उन लोगों को देखते थे, जिनके साथ वे भूमि और स्वतंत्रता की लूट कर रहे थे, उस घृणा और तिरस्कार को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना असंभव था। ये भावनाएँ मुख्य रूप से मानव प्रवृत्ति के उस सबसे अकाट्य और अतार्किक, नस्ल विरोध से उत्पन्न होती हैं, जो महान मूल्य के अनगिनत मार्गों में बंट पाती हैं, क्योंकि वे हमें एक साथ मिलकर एक सही तस्वीर बनाने में सक्षम बनाती हैं कि वे मूल निवासी क्या रहे होंगे, और किस तरह से वे मुख्य रूप से उनके विजेताओं के विपरीत। रंग और बनावट में अंतर सबसे पहले हम पर प्रहार करता है, और इसमें, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, हम जाति भेद की शुरुआत का पता लगाते हैं। "दस्युओं को नष्ट करके, इंद्र ने आर्य रंग की रक्षा की," एक कवि कृतज्ञतापूर्वक घोषणा करता है। "इंद्र," एक और कहता है, "आर्य उपासक की युद्ध में रक्षा की, उसने मनु के लिए अधर्म को वश में किया, उसने काली त्वचा पर विजय प्राप्त की।" "उन्होंने [इंद्र] दस्युओं को अपनी आदत के अनुसार हराया ... उन्होंने अपने गोरे [या गोरे] दोस्तों के साथ भूमि पर विजय प्राप्त की। . . उनके आर्य विजेताओं द्वारा दिए गए अन्य नाम "बकरी-नाक" और "नाक रहित" (एनासो, स्पष्ट रूप से "फ्लैट-नाक" का अतिशयोक्ति) हैं, जबकि आर्य देवताओं की उनकी सुंदर नाक के लिए प्रशंसा की जाती है। कोई पवित्र आग नहीं, पागल देवताओं की पूजा करने की, कच्चा मांस खाने की, और अंत में, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ख़तरनाक जादूगर माना जाता था: "तू [इंद्र] ने ऋषि के ख़िलाफ़ दिसा के जादू को शक्तिहीन बना दिया है।" यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा के अंतर ने उस बाधा को पूरा किया जिसे बाद में विजेताओं ने अगम्य बनाने का प्रयास किया।
यद्यपि “आर्य” के विरुद्ध “दस्यु” या “दास” शब्द और “द्वेज” के विरुद्ध “शूद्र” शब्दों का, होना एक पूर्ण रूप से स्थापित और बोधगम्य तथ्य है, अतः यह समझना एक ग़लती होगी कि "दस्यु" या "शूद्र" किसी विशेष जाति के नाम हैं। वास्तव में ये श्ब्द उन सभी जातियों के लिए बोले जाते थे, जो आर्य नहीं थे। ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन काल में, उन सभी लोगों को (Barbarians) "बर्बर" के नाम से जाना जाता था, जो ग्रीक या रोमन नहीं थे।
प्रो.ऐडवर्ड रैप्सन “कैम्ब्रिज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया” में लिखते हैं :
“The poets of the Rigveda know nothing of caste in the later and stricter sense of the word; but they recognise that there are divers orders of men — the priests (Brahma or Brahmana), the nobles (Rajanya or Ksha- triya), the tillers of the soil (Vic or Vaicya), and the servile classes (Shudra). Between the first three and the fourth there is a great gulf fixed. The former are conquering Aryans: the latter are subject Dasyus. The difference between them is one of colour {varna ) : the Aryans are collectively known as ^ the light colour,' and the Dasyus as ^ the dark colour.'” (Cambridge History of India, Vol. l, Page 54)
“ऋग्वेद के कवि उन कठोर अर्थों में जाति से परिचित न थे, जो उन शब्दों ने बाद में ग्रहण कर लिए; लेकिन वे मानते हैं कि मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं - पुजारी (ब्रह्मा या ब्राह्मण), कुलीन (राजन्य या क्षत्रिय), ज़मीन जोतने वाले किसान (विश या वैश्य), और दास वर्ग (शूद्र)। पहले तीन वर्गों और चौथे वर्ग के बीच एक चौड़ी खाई है। पहले तीनों विजेता आर्य हैं: बाद वाले विजित दस्यु हैं। उनके बीच रंग का अंतर है। आर्य आमतौर पर गोरी चमड़ी वाले लोग समझे जाते हैं और दस्यु काली चमड़ी वाले।”
इन साक्ष्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जिन लोगों को भारतीय क़ानून में शूद्र ठहराया गया है, वे वास्तव में ग़ैर-आर्य विजित जातियां हैं। इसलिए उनके लिए हिंदू धर्म शास्त्रों में जो क़ानून निर्धारित किए गए हैं, वे उन जातियों के प्रति हिंदू धर्म के व्यवहार को दर्शाते हैं जो प्राजित और होकर उसके शासन के अधीन हो जाते हैं।
(2) यहूदी धर्म
यहूदी धर्म के नियमों की खोज और शोध में हमें उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि हिंदू धर्म के नियमों को खोजने में करना पड़ा। केवल एक किताब, ‘तोराह’ को लेकर हम यहूदी धर्म की शिक्षाओं और उसके नियमों का पता लगा सकते हैं और उसमें यहूदी धर्म को उसके असली रंग में देखा जा सकता है। हालाँकि बाद में यहूदी विद्वानों ने यहूदी क़ानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए कई किताबें लिखीं हैं, जो संहिता के विवरण और व्याख्या पर आधारित हैं, जैसे कि अकीबा इब्ने यूसुफ की मिश्नाह और मिडराश, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखी गईं। तलमूद, जो मिश्नाह और गेमारा, को मिलाकर 6ठी शताब्दी ईस्वी में संकलित की गई। इसाक अल-फ़ासी की “हलाखा”, जो 11वीं शताब्दी में लिखी गयी और इसे तलमुदिक क़ानूनों का सबसे अच्छा संस्करण माना जाता है। मूसा मैमोनी द्वारा मिश्नाह तोराह, जिसे बारहवीं शताब्दी के अंत में संकलित किया गया था। याकूब बिन अशहर की तूर, जो चौदहवीं शताब्दी की यादगार है, और यूसुफ कारो की शुलखान अरवख़, जो सोलहवीं शताब्दी में लिखी गयी, और जिसमें यहूदी रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के सभी नियम प्राचीन परंपराओं के अनुसार संकलित हैं। हमारे लिए, ये किताबें उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि उनमें से किसी पर भी यहूदियों के सभी संप्रदायों की सहमति नहीं है, और न उनमें से किसी को यहूदी धर्म का आधार ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं कई बार यहूदियों ने इन किताबों से विमुखता दिखायी है और तोराह के सिवा किसी को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसलिए, हम इन सभी किताबों की उपेक्षा करते हैं और युद्ध के मामले में केवल तोराह का उल्लेख करते हैं।
यहां यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि तोराह के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे वह उस तोराह के बारे में नहीं होगा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, बलकि उस तोराह के बारे में होगा जो अज दुनिया भर में यहूदियों के पास उनके धर्मग्रंथ के रूप में मौजूद है और जिसे “ओल्ड टेस्टामेंट” के नाम से जाना जाता है। हमारा शोध यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट की पेंटाटेन्थ (5 किताबें) मूल तोराह नहीं हैं। मूल तोराह तो नष्ट हो चुकी है। इस सिद्धांत की पुष्टि ख़ुद मौजूदा “ओल्ड टेस्टामेंट” को पढ़ने से होती है। उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि हज़रत मूसा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में हज़रत येशु की सहायता से तोराह को संकलित किया और उसे एक संदूक में रखवा दिया था:
“मूसा ने जब क़ानून की सारी बातें किताब में लिख लीं तो उसके फौरन बाद उसने लेवियों को, जो यहोवा के क़रार का संदूक़ ढोया करते थे, यह आज्ञा दी: “तुम क़ानून की यह किताब लेना और इसे अपने परमेश्वर यहोवा के क़रार के संदूक़ के पास रखना और यह तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाह ठहरेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ढीठ और बाग़ी लोग हो। आज जब मैं ज़िंदा हूँ तब तुम यहोवा के ख़िलाफ़ इतनी बग़ावत कर रहे हो, तो मेरी मौत के बाद और कितनी ज़्यादा बग़ावत करोगे!” (व्यवस्थाविवरण,31 : 24-27)
उनकी मृत्यु के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब बख़्ते नस्र ने बैतुल मक़दिस को आग लगा दी, तो वह पवित्र सन्दूक उन सभी किताबों सहित जल गया, जिन्हें हज़रत मूसा के बाद उनकी शरीअत के आधुनिकीकरणकर्ताओं ने संकलित किया था। इस विनाश के ढाई सौ साल बाद, जब हज़रत उज़ैर (एज़्रा) ने बनी इसराईल के पुरोहितों, धर्मशास्त्रियों और लावियों के साथ मिलकर आकाशीय प्रेरणा से इस किताब को फिर से संकलित किया, लेकिन उस युग की कई घटनाओं ने इस नए संस्करण को भी उसके मूल रूप में बचा नहीं रहने दिया।
सिकंदर महान की विश्व विजय जब ग्रीक शासन के साथ-साथ ग्रीक कला, विज्ञान और आचार-विचार को भी लेकर पूर्व में फैल गई, तो 280 ईसा पूर्व में, तोराह की सभी किताबों को ग्रीक भाषा में स्थानांतरित कर दिया गया और धीरे-धीरे मूल हिब्रू संस्करण अप्रचलित हो गया और यह ग्रीक अनुवाद प्रचलन में आ गया। इसलिए आज जो तोराह हमारे सामने है वह किसी भी तरह से हज़रत मूसा तक नहीं पहुंचती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वर्तमान तोराह में मूल तोराह का कुछ भी अंश शामिल नहीं है या यह पूरी तरह से नक़ली है। वास्तव में हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि इस तोराह में दूसरी चीज़ें घुल-मिल गई हैं, और संभव है कि उसमें से कुछ चीज़ें ग़ायब हो गई हों। आज जो कोई भी खुली आंखों से इस किताब का अध्ययन करेगा उसे स्पष्ट रूप से लगेगा कि इसमें ईश्वरीय शब्दों के साथ यहूदी विद्वानों की टीकाएं, बनी इसराईल का राष्ट्रीय इतिहास, इसराईली न्यायविदों के क़ानूनी शोध और अन्य बहुत सी चीज़ें अल्लाह के वचन के साथ गडमड हो गई हैं, जिन्हें ईश्वरीय शब्दों से अलग कर के अल्लाह के कलाम को छांटना एक कठिन काम है। इसके साथ ही हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पवित्र क़ुरआन के मुताबिक़ तोराह का दीन वही है जो स्वयं क़ुरआन का दीन है, और मूसा अलैहिस्सलाम ठीक उसी तरह इस्लाम के पैग़म्बर थे, जिस तरह हज़रत मुहम्मद सल्ल. हैं। बनी इसराईल शुरुआत में उसी दीन इस्लाम के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अस्ल दीन में अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ जोड़कर या घटाकर एक नई धार्मिक व्यवस्था “यहूदी धर्म” के नाम से बना ली। अतः हम यहां जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह यही यहूदी धर्म है न कि वह दीन जो पैग़म्बर मूसा लाए थे।
युद्ध का उद्देश्य
तोराह में, लड़ाइयों का बहुत बार उल्लेख किया गया है और जगह-जगह इसके आदेश दिए गए हैं। लेकिन एक मक़सद को छोड़कर जिसका वर्णन व्यवस्थाविवरण अध्याय 2 और गिनती अध्याय 33 में किया गया है और किसी मक़सद का कोई संकेत हमें नहीं मिलता। इस उद्देश्य का वर्णन गिनती की किताब में इस प्रकार किया गया है:
“फिर मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा ने मूसा से कहा, “इस्त्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार हो कर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना; और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूतिर्यों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना। और उस देश को अपने अधिकार में ले कर उस में निवास करना, क्योंकि मैं ने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना; अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हैं उन को थोड़ा भाग देना; जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिये निकले वही उसका भाग ठहरे; अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना।” (गिनती की किताब, 33:50-54)
और व्यवस्थाविवरण में है:
“अब तुम लोग उठ कर कूच करो, और अर्नोन के नाले के पार चलो; सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ; इसलिये उस देश को अपने अधिकार में लेना आरम्भ करो, और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सभों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा; वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे।” (2:24)
“परन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने हम को अपने देश में से हो कर चलने न दिया; क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिये कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझ से कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ; उस देश को अपने अधिकार में लेना आरम्भ कर। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया, और हमारा साम्हना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ा आया। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हम ने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हम ने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल-बच्चों समेत यहाँ तक सत्यनाश किया कि कोई न छूटा; परन्तु पशुओं को हम ने अपना कर लिया, और उन नगरों की लूट भी हम ने ले ली जिन को हम ने जीत लिया था।” (2:30-35)
तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले; और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा साम्हना करने को निकल आया, कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझ से कहा, उस से मत डर; क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ; और जैसा तू ने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है वैसा ही उस से भी करना। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया; और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उन में से कोई भी न बच पाया। उसी समय हम ने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हम ने उस से न ले लिया हो, इस रीति अर्गोब का सारा देश, जो बाशान में ओग के राज्य में था और उस में साठ नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे, और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह, और फाटक, और बेड़े थे, और इन को छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हम ने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था वैसा ही हम ने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियोंऔर बाल-बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परन्तु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हम ने अपनी कर ली। (3:1-7)
इन गद्यांशों से स्पष्ट होता है कि तोराह के युद्ध का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार है। किसी देश के निवासियों को तलवार के बल पर प्राजित करना और बलप्रयोग के आधार पर उनके धन-संपत्ति और यहाँ तक कि उनके जीवन पर भी अधिकार कर लेना उसकी दृष्टि में जायज़ है और उसके अनुसार यही क्रोध और प्रभुत्व धरती के उस उत्तराधिकार का अर्थ है, जिसे ख़ुदा ने इसराईलियों को देने का वादा किया है:
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ۔ (القرآن، سورۃ الانبیاء :105)
“और हमने ज़बूर में याददेहानी के बाद लिख दिया है कि धरती के उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी बन्दे होंगे।” (क़ुरआन, 21:105)
एक अन्य स्थान पर कहा:
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ (القرآن، سورۃ الاعراف :128)
मूसा ने अपनी क़ौम से कहाः अल्लाह से सहायता माँगो और धैर्य से म लो, वास्तव में, धरती अल्लाह की है, वह अपने बन्दों में जिसे चाहे, उसका वारिस (उत्तराधिकारी) बना देता है और परलोक का घर उन्हीं के लिए है, जो आज्ञाकारी हों। (क़ुरआन, 7:128)।
लेकिन इस उत्तराधिकार की कल्पना तोराह की कल्पना से बिल्कुल अलग है। तोराह भूमि का उत्तराधिकार केवल बनीइसराईल को देता है, जैसा कि ‘संख्या’ (33:50) से स्पष्ट है। लेकिन कुरआन इसे किसी एक जाति या राष्ट्र का नहीं, बल्कि आज्ञाकारी बन्दों का अधिकार ठहराता है। तोराह में, भूमि के उत्तराधिकार (विरासत) का अर्थ यह है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के घर, संपत्ति, जीवन और प्रतिष्ठा का स्वामी बन जाए, और इसे नष्ट करके, ख़ुद उसकी जगह जा बसे। लेकिन क़ुरआन में अल्लाह की ओर से किसी क़ौम को भूमि का उत्तराधिकार दिए जाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने आज्ञाकारी होने के आधार पर उस क़ौम को अपनी ख़िलाफ़त और हुकूमत के लिए चुना है और अपनी ज़मीन का प्रबंध उसे सौंप दिया है, ताकि वह अन्याय को मिटा दे और उसके स्थान पर न्याय की व्यवस्था स्थापित करे। फिर तोराह में जमीन का उत्तराधिकार पाने के लिए युद्ध का आदेश दिया गया है, लेकिन क़ुरआन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि अमुक भूमि तुम्हारी राष्ट्रीय विरासत है, इसलिए तुम युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करो। तो तोराह का भूमि का उत्तराधिकार खुला अधिग्रहण और साम्राज्य विस्तार है। इस्लाम के अल्लाह की खातिर जिहाद के विपरीत, इसके युद्ध का उद्देश्य केवल देश और धन प्राप्त करना और अन्य राष्ट्रों पर एक विशेष राष्ट्र की श्रेष्ठता स्थापित करना है।
युद्ध की सीमाएं
हमें युद्ध की सीमाओं और नियमों के बारे में तोरात में अधिक विवरण नहीं मिलता है। फिर भी इससे इतना मालूम होता है कि यहूदी धर्म अपने अनुयायियों को दुश्मन से निपटने के लिए किस तरह का व्यवहार करने का निर्देश देता है। इसके लिए निम्नलिखित नियम पढ़ने योग्य हैं:
किताब में शामिल हैं:
जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उनके निकट जाए, तब पहिले उस से सन्धि करने का समाचार दे। और यदि वह सन्धि करना अंगीकार करे और तेरे लिये अपने फाटक खोल दे, तब जितने उस में होंवे सब तेरे आधीन हो कर तेरे लिये बेगार करने वाले ठहरें। परन्तु यदि वे तुझ से सन्धि न करें, परन्तु तुझ से लड़ना चाहें, तो तू उस नगर को घेर लेना; और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उस में के सब पुरूषों को तलवार से मार डालना। परन्तु स्त्रियां और बालबच्चे, और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिये रख लेना; और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। (20:10-14)
“ परन्तु जो नगर इन लोगों के हैं, जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को ठहराने पर है, उन में से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परन्तु उन को अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों, और यबूसियों, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है;।” (20:16-17)
“जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिये उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चला कर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिये उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उन को भी घेर रखे?”(20:19)
“और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले; तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना; उन से न वाचा बान्धना, और न उन पर दया करना। और न उन से ब्याह शादी करना, न तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिये ब्याह लेना। क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी, और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी; और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, और वह तुझ को शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूत्तिर्यों को काट काटकर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना।” (7:2-5)
“देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उस में जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वा टीलों पर, वा किसी भांति के हरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सभों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना; उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूत्तिर्यों को आग में जला देना, और उनके देवताओं की खुदी हुई मूत्तिर्यों को काटकर गिरा देना, कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं।” (12:1-3)।
किताब निर्गमन में है:
“जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूं उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, और यबूसी लोगों को निकालता हूं। इसलिये सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बान्धना; कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिये फंदा ठहरे। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, और उनकी अशेरा नाम मूतिर्यों को काट डालना;” (34: 11-13)
किताब संख्या में है:
“फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्त्राएलियों का पलटा ले; बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरूषों को युद्ध के लिये हथियार बन्धाओ, कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उन से यहोवा का पलटा ले। इस्त्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हज़ार पुरूषों को युद्ध करने के लिये भेजो। तब इस्त्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हज़ार पुरूष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिये हथियार-बन्द बारह हज़ार पुरूष।प्रत्येक गोत्र में से उन हज़ार हज़ार पुरूषों को, और एलीआजर याजक के पुत्र पीनहास को, मूसा ने युद्ध करने के लिये भेजा, और उसके हाथ में पवित्रस्थान के पात्र और वे तुरहियां थीं जो सांस बान्ध बान्ध कर फूंकी जाती थीं। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरूषों को घात किया। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एवी, रेकेम, सूर, हूर, और रेबा नाम मिद्यान के पांचों राजाओं को घात किया; और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्त्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल-बच्चों समेत बन्धुआई में कर लिया; और उनके गाय-बैल, भेड़-बकरी, और उनकी सारी सम्पत्ति को लूट लिया। और उनके निवास के सब नगरों, और सब छावनियों को फूंक दिया; तब वे, क्या मनुष्य क्या पशु, सब बन्धुओं और सारी लूट-पाट को ले कर यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर, मोआब के अराबा में, छावनी के निकट, मूसा और एलीआजर याजक और इस्त्राएलियों की मण्डली के पास आए॥ तब मूसा और एलीआजर याजक और मण्डली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति-शतपति आदि, सेनापतियों से, जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित हो कर कहने लगा, क्या तुम ने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखे, बिलाम की सम्मति से, पोर के विषय में इस्त्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मण्डली में मरी फैली। सो अब बाल-बच्चों में से हर एक लड़के को, और जितनी स्त्रियों ने पुरूष का मुंह देखा हो उन सभों को घात करो। परन्तु जितनी लड़कियों ने पुरूष का मुंह न देखा हो उन सभों को तुम अपने लिये जीवित रखो। (31:1-18)
यहोशू की किताब में:
“और क्या पुरूष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़-बकरी, गदहे, और जितने नगर में थे, उन सभों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरूषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जा कर उसको और जो उसके पास हों उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जा कर राहाब को, और उसके माता-पिता, भाइयों, और सब को जो उसके यहां रहते थे, वरन उसके सब कुटुम्बियों को निकाल लाए, और इसराईल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को, और जो कुछ उस में था, सब को आग लगाकर फूंक दिया; केवल चांदी, सोना, और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उन को उन्होंने यहोवा के भवन के भण्डार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया; और आज तक उसका वंश इसराईलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उन को उसने छिपा रखा था।” (6:21-25)
“और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इसराईली ऐ के सब निवासियों मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहां तक कि उनका अन्त ही हो गया, तब सब इसराईलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरूष, सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे बारह हज़ार थे, और ऐ के सब पुरूष इतने ही थे। क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों सत्यानाश न कर डाला तब तब उसने अपना हाथ, जिस से बर्छा बढ़ाया था, फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी इसराईलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फूंकवा दिया, और उसे सदा के लिये खंडहर कर दिया: वह आज तक उजाड़ पड़ा है।” (8:23-28)।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि यहूदी धर्म अपने दुश्मनों को दो श्रेणियों में बांटता है। एक जिसे ख़ुदावंद ने इसराईल की सन्तान को मीरास में नहीं दिया। दूसरे वे जिनको उसने उनकी मीरास में दे दिया है। दोनों के साथ उनका व्यवहार अलग-अलग तरह का है।
पहले प्रकार के शत्रुओं के लिए उनका आदेश यह है कि पहले उन्हें शांति का संदेश दिया जाए और अगर वे उसे स्वीकार करते हैं और अपने देश को बनी इसराईल को सौंप देते हैं, तो उन्हें ग़ुलाम और सेवक बना लिया जाए। परन्तु अगर वे सन्धि न करें तो उनके साथ युद्ध करना चाहिए और विजय होने पर उनके सब पुरुषों को मार डालना चाहिए, स्त्रियों और बच्चों को दास बना लेना चाहिए और उनकी सम्पत्ति ज़ब्त कर लेनी चाहिए। युद्ध के दौरान बागों और खेतों और फलों के पेड़ों का विनाश निषिद्ध है, इसलिए नहीं कि यह एक भ्रष्ट कार्य है, बल्कि इसलिए कि इस तरह के विनाश से जीत की स्थिति में विजेता को लाभ नहीं होगा।
दूसरे प्रकार के शत्रुओं को वह सभी मानव अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित कर देता है। उसका आदेश यह है कि उन जातियों के साथ कोई शांति और सन्धि न की जाए, उनके विरुद्ध युद्ध किया जाए, उनकी बस्तियाँ उजाड़ दी जाएँ, उनके खेत-बगीचे, भवन और पूजा-स्थल नष्ट कर दिए जाएँ। उनकी स्त्री, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि जानवरों को भी मार डाला जाए और ज़मीन से उनका नाम और निशान तक मिटा दिया जाए। इस युद्ध का उद्देश्य केवल यह बताया गया है कि विरासत में मिले राष्ट्रों का पूर्ण विनाश कर दिया जाए। उन जातियों के सामने ऐसी कोई शर्त पेश ही नहीं की गई, जिसे पूरा करने के बाद उनका छुटकारा संभव हो।
इस शिक्षा पर किसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है, यह अपने ऊपर स्वयं टिप्पणी कर रही है। इस पर जीवंत टिप्पणी फ़िलिस्तीन में इसराईल राज्य है, जो भूमि की विरासत की इसी कल्पना पर स्थापित किया गया था, और बीसवीं शताब्दी में, उसने अरबों के साथ वही कुछ कर दिखाया जिसका निर्देश तोराह द्वारा दिया गया था।
(3) बौद्ध धर्म
यहां तक उन धर्मों का उल्लेख था जिनसे इस्लाम का मतभेद युद्ध के औचित्य या अनाौचित्य में नहीं, बल्कि उसके नैतिक और व्यावहारिक स्वरूप में था। अब दूसरे प्रकार के वे धर्म हैं जो युद्ध के ही ख़िलाफ़ हैं और इस आधार पर इस्लाम से असहमति रखते हैं कि वह तलवार से जिहाद की अनुमति ही क्यों देता है। उन धर्मों में ऐतिहासिक क्रम की दृष्टि से प्रथम स्थान बौद्ध धर्म का है।
बौद्ध धर्म के स्रोत
इस विषय में बौद्ध धर्म की पद्धति की जांच करने से पहले, यह ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमारे पास यह सुनिश्चित करने का कोई साधन नहीं है कि वास्तव में गौतम बुद्ध की शिक्षा क्या थी। बुद्ध ने वास्तव में अपने जीवनकाल में क्या सिखाया इसे जानने का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। बुद्ध ने अपने जीवनकाल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने अपने स्थापित धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का एक संग्रह भी संकलित नहीं कराया, जिससे उनके अपने शब्दों में उनकी शिक्षाओं का पता लगाया जा सके। इतिहास साबित करता है कि उनके अनुयायियों में से किसी ने भी उनके जीवनकाल में या उसके तुरंत बाद के ज़माने में कभी भी उनकी शिक्षाओं को संहिताबद्ध करने का प्रयास नहीं किया। कुछ परम्पराओं से ज्ञात होता है कि उनकी मृत्यु के बाद राजगृह में एक विशाल सभा हुई थी जिसमें उनके एक-दो विशिष्ट शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं पर मौखिक व्याख्यान दिया था । साथ ही उन्हीं परम्पराओं से यह भी सिद्ध होता है कि उन व्याख्यानों को लिखित रूप में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। दूसरी बात यह कि, ऐतिहासिक तौर पर यह भी पूरी तरह सिद्ध नहीं होता है कि उक्त परिषद वास्तव में हुई भी थी या नहीं। महायान महापरिनिर्वाण सूत्र, जो बुद्ध के जीवन और बाद की परिस्थितियों को जानने के लिए हमारे पास सबसे प्रामाणिक स्रोत है, उक्त परिषद के विषय पर पूरी तरह से मौन है। अब रहीं वर्तमान पुस्तकें, जो इस धर्म के बारे में जानकारी का हमारा एकमात्र स्रोत हैं, ये सभी गौतम बुद्ध के बहुत बाद लिखी गई हैं। उनकी मृत्यु के बाद एक शताब्दी बीत चुकी थी जब वैशाली में इस धर्म के धर्मगुरुओं की एक बैठक हुई थी और बहुत बहस के बाद इसके सिद्धांतों, मान्यताओं और नियमों को तैयार करने का प्रयास किया गया था। लेकिन दीपवंस के लेखक हमें बताते हैं कि इसमें भिक्षुओं ने मूल धर्म के सिद्धांतों को बदल दिया, इसकी कई मान्यताओं और आदेशों को संशोधित और निरस्त कर दिया और मूल सूत्रों को बदल कर नए सूत्र बना लिए।(sacred books of the Buddhists : Maxmular)
उस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म को लिखित रूप में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और यह प्रक्रिया पहली शताब्दी ई. तक यानी 400 वर्षों तक चलती रही। लेकिन बाद के ज़माने में यह धर्म फिर से विकृतियों का शिकार हुआ, यहाँ तक कि इसके मूलभूत सिद्धांत भी बदल गए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब माना जाता है कि एक अमर अस्तित्व है, जो सर्व जगत से श्रेष्ठ है और जिसकी बुद्ध के रूप में केवल एक भौतिक अभिव्यक्ति हुई है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन अब स्वीकार कर लिया गया है कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार स्वर्ग है और बुरे कर्मों का दंड नरक। प्रारम्भिक बौद्ध धर्म में सन्यासी जीवन के नियम अत्यंत कठोर थे, किन्तु अब उनमें ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन करके नर्म कर दिया गया है। बौद्ध धर्म में यह अंतिम विकृति कनिष्क काल के दौरान हुई जो पहली शताब्दी ईस्वी में गुज़रा है। इतिहास से ज्ञात होता है उसके समय में कश्मीर में जो कौंसिल हुई थी उसी में इस विकृति के बाद बौद्ध धर्म के नियम संकलित किये गए थे। इन आधुनिक क़ानूनों को एक छोटे से संप्रदाय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म के बड़े वर्ग, जिसे महायान संप्रदाय कहा जाता है, द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया।
इससे यह स्पष्ट है कि आज बौद्ध धर्म के अनुयायी जिसे “धार्मिक ग्रंथ” कहते हैं, वास्तव में उसमें बौद्ध धर्म मौजूद नहीं है। और हम किसी भी प्रमाण के आधार पर निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा क्या थी। कुछ हद तक अगर भरोसा किया जा सकता है तो केवल उन किताबों पर, जो कनिष्क काल की अंतिम विकृति से बच गईं, और वे तीन हैं, जो संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहलाती हैं:
(1) विनय पिटक : यह तपस्वी जीवन के नियमों का संग्रह है, और यह 350 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 250 ईसा पूर्व तक के काल में इसकी रचना हुई है, लेकिन इसके रचयिता या लेखकों का पता नहीं मिलता।
(2) सुत्त पिटक : इसमें मोक्ष के नियम या बौद्ध नैतिक दर्शन पर गौतम बुद्ध के कथनों का संग्रह किया गया है। इस संग्रह के लेखक और लेखन के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती।
(3) अभिधम्म पिटक : य़ह अधिकतर बौद्ध दर्शन, नैतिकता और तत्वमीमांसा पर आधारित है। इसके बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से पहले अस्तित्व में था।
आगामी पृष्ठों में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जो भी कहेंगे वह वास्तव में उस बुद्ध जी के बारे में होगा जिन्हें ये पुस्तकें प्रस्तुत करती हैं, न कि उस गौतम बुद्ध के बारे में जिनको हम नहीं जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या शिक्षा दी है।
अहिंसा की शिक्षा
बौद्ध धर्म एक अहिंसावादी धर्म है। इसमें प्रत्येक जीव को निर्दोष माना गया है और मनुष्य से लेकर छोटे से छोटे कीट-पतंग तक प्रत्येक जीव के जीवन के अधिकार को इस अर्थ में स्वीकार किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में उसका हनन नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध के दस आदेशों में पहला आदेश यह है “किसी भी जीव की हत्या मत करो।” एक भिक्षु जो जानबूझकर किसी जीव की हत्या करता है, वह उसके क़ानून में एक अक्षम्य अपराध का दोषी है। हद तो यह है कि वह भिक्षुओं को बरसात के तीन महीनों के दौरान एकांतवास से निकलने से भी मना करता है, ताकि जमीन पर रेंगने वाले कीड़े रौंदे न जा सकें। इन कठोर अहिंसावादी आदेशों के साथ युद्ध की अनुमति देना तो दूर की बात है, उसकी कल्पना भी असंभव है। जब उसकी दृष्टि में जीवन का सम्मान इतना अधिक है, तो उसे अनिवार्य रूप से एक ऐसे कार्य को घोर घृणा के दृष्टि से देखना चाहिए जिसमें कीड़े-मकोड़ों की नहीं, मनुष्यों की हज़ारों जानों की बलि चढ़ जाती है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म ने एक भिक्षु को इस की अनुमति भी नहीं दी है कि वह युद्ध के मैदान में दर्शक के रूप में भी जाए और रक्तपात देखे। पिक्तीय धम्म के 48वीं धारा में है:
“जो भिक्षु बिना किसी उचित कारण के युद्ध के लिए तैयार सेना को देखने जाता है, वह पिक्तीय अपराध का दोषी होगा।”
धारा 49 और 50 के शब्द ये हैं :
अगर भिक्षु के सेना की ओर जाने का कोई उचित कारण हो तो वह केवल दो या तीन रातों तक वहाँ ठहर सकता है। अगर वह उससे अधिक ठहरे, तो यह पिक्तीय है।”
“और अगर वह दो या तीन रातों तक वहां ठहरने के दौरान युद्ध के मैदान के गठन या बलों की गणना या योद्धाओं के संरेखण के अवसर पर वहां जाए, तो यह भी पिक्तीय अपराध है।”
बौद्ध दर्शन
इन आदेशों से बौद्ध धर्म का युद्ध संबंधी सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इस धर्म की अच्छाई और बुराई का सही आकलन करने के लिए केवल इन संक्षिप्त नियमों को जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दर्शन की पूरी व्यवस्था को समझना आवश्यक है, जिसका एक भाग अहिंसा की यह मान्यता है।
अहिंसा वास्तव में मानव जीवन को उस विशेष आकार में ढालने और उस विशेष पथ पर ले जाने के साधनों में से एक है जिसे बुद्ध ने मनुष्य के लिए पसंद किया है। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि वह कौन सा आकार है जिसमें बुद्ध मानव जीवन को ढालना चाहते हैं? वह कौन सी मंज़िल है जिसे उन्होंने अपना आदर्श बनाया है? और इस उद्देश्य के लिए वे किन व्यावहारिक साधनों का उपयोग करते हैं? इन मुद्दों को समझे बिना अहिंसा की सच्ची भावना और मानव जीवन पर उसके गहरे प्रभावों को समझना मुश्किल है।
गौतम बुद्ध ने मानव जीवन का अध्ययन जिस दृष्टिकोण से किया है, वह दुनिया के अन्य चिंतकों और धर्म व नैतिकता के विद्वानों और शिक्षकों के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। गौतम बुद्ध ने यह समझने का कोई प्रयास ही नहीं किया कि मनुष्य दुनिया में क्यों पैदा हुआ है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से, वे इस विषय पर भी चर्चा नहीं करते कि इस संसार में मनुष्य के जीने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है, जिसपर चलकर समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। उन्होंने अपना सारा ध्यान केवल इस प्रश्न को हल करने में लगा दिया है कि मानव जीवन में परिवर्तन और क्रांति क्यों होती है? बाल्यावस्था, यौवन, बुढ़ापा, स्वास्थ्य, बीमारी, जन्म, मृत्यु, दुख, सुख, राहत, क्लेश और इसी प्रकार की विभिन्न स्थितियों का कारण क्या है? और इस चक्रव्यूह से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? मनुष्य के समस्त व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उन्होंने केवल इसी एक प्रश्न को ध्यान देने योग्य पाया है और अन्य सभी व्यावहारिक और वैचारिक मुद्दों पर उन्होंने अपनी आँखें पूरी तरह से बंद कर ली हैं।
इस मूल प्रश्न पर कई वर्षों तक चिंतन मनन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपने आप में जीवन ही एक पीड़ा है जिसमें मनुष्य फंस गया है और जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जितने भी परिवर्तनों से गुज़रता है, वे सब इसी पीड़ा का हिस्सा हैं। उसका संसार में आने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह व्यर्थ और बेकार ही जन्म लेता है। या फिर अगर उसका कोई काम है तो वह केवल पीड़ा सहन करना और तड़पना ही है। अतः यह संसार उसके रहने का स्थान नहीं है। यहाँ उसके लिए वास्तव में कोई आराम और आनंद नहीं है। क्योंकि हर सुख के पीछे एक दुख, हर उदय के पीछे एक अस्त और हर जन्म के पीछे एक मृत्यु लगी हुई है। और यह सब परिवर्तन और क्रांति की एक सतत प्रक्रिया के अधीन है, जो स्वयं एक समस्या है।
मनुष्य इस पीड़ा में क्यों घिरा हुआ है? गौतम बुद्ध इसका उत्तर यह देते हैं कि इच्छा, भावना और चेतना उसे जीवन में कष्ट देती हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण मनुष्य का संसार से संबंध स्थापित हो जाता है और यही संबंध उसे बार-बार संसार में लाता है। वह बार-बार उसे एक योनि से दूसरे योनि, एक रूप से दूसरे रूप में, और एक जीवन से दूसरे जीवन में लिए फिरता है और जब तक उसके गले से इच्छाओं का फंदा नहीं हटता, तब तक वह बार-बार मरने और दोबारा जीवित होकर किसी न किसी रूप में जन्म लेने के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता।
फिर इस संकट से, जीवन के इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? इस प्रश्न का समाधान गौतम बुद्ध ने केवल एक शब्द “निर्वाण” से किया है। उनका कहना है कि जब जीवन दुख है और इच्छा उस दुख की जड़ है, तो मनुष्य के लिए वास्तविक राहत केवल शून्यता और अस्तित्वहीनता में निहित है, और वह इच्छा, भावना और चेतना के पूर्ण विनाश से प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को संसार के सभी क्षेत्रों से कट जाना चाहिए। किसी चीज़ का प्रेम, किसी चीज़ की चाह, इस संसार की किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण वह अपने हृदय में न रखे और अपने समस्त मनोभावों, और इच्छाओं को इस प्रकार नष्ट कर दे कि इस दुनिया से उसका कोई संपर्क और संबंध शेष न रहे, जो उसे दोबारा यहां वापस लाने का कारण बने। इस प्रकार वह “अस्तित्व” के बंधन से निकल जाएगा और “अस्तित्वहीनता” या विनाश की स्थिति में पहुंच जाएगा। यही “निर्वाण” है, और यह गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, या होना चाहिए।
अब चौथा प्रश्न यह है कि निर्वाण प्राप्त करने का तरीक़ा क्या है? यहां पहुंचकर बौद्ध धर्म व्यावहारिक रूप धारण करता है, इसने निर्वाण तक पहुंचने के लिए आठसूत्री उपाय प्रस्तुत किया है, जिसे गौतम बुद्ध के अष्टागिंक मार्ग कहा जाता है और वह संक्षेप में इस प्रकार है:
यहाँ पर सम्यक का अर्थ हैं – उचित.
सम्यक दृष्टि
पांच इन्द्रियों में आँख भी एक हैं. इन्द्रियों के ज़रिये ही बाहरी वस्तुओं का आभास होता हैं। नेत्र के ज़रिये देखने पर जो महसूस होता है, और जिस भाव की अनुभूति होती हैं, इन सभी का उद्भव इच्छाओं के ज़रिये होता है। केवल दृष्टि के ज़रिये मनुष्य लोभ, मोह, काम में बांध जाता है. इसके लिए बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि (उचित दृष्टी) को मोक्ष का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है।
पूर्ण संकल्प
अर्थात् सुखों को त्यागने का और दूसरे जीवों को नुक़सान पहुँचाने से बचने का दृढ़ निर्णय।
पूर्ण प्रयास
बुद्ध का अगला सबसे महत्वपुर्ण क़दम है धर्म के उपदेशों के अनुसार कार्य करने का प्रयास।
सम्यक वचन
आचरण की झलक बोले गये वचनों से मिलती है, इसलिए मधुर वाणी के साथ साथ वचनों को सम्यक होना चाहिए। बुरी भाषा, व्यर्थ की गपशप, चुग़ली और झूठ से बचना चाहिए।
सम्यक जीविका
इस का अर्थ है वैध तरीक़ों से आजीविका कमाना। जीवन को चलाने के लिए कुछ मुलभुत चीजो की आवश्यकता होती है, लोग अपनी आजीविका के लिए चीज़ें कहाँ से जूटाते हैं यह महत्वपूर्ण है। जीविका के साधन को सम्यक ढंग से जूटाना चाहिए, क्योंकि यही साधन शरीर का पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनको सम्यक होना आवश्यक है।
सम्यक कार्य
सब कुछ कर्म पर निर्भर करता है। हर किसी को किये गए कर्मो का फल भोगना पड़ता हैं। इसलिए कर्म ऐसे हों कि उनका फल सदैव पुन्य की और आश्रित हो। केवल सद्कर्म करना और अनैतिकता, जीवहत्या, बेईमानी और विश्वासघात से बचना चाहिए।
सम्यक स्मृति
अर्थात अपने पिछले कर्मों को याद रखना, ताकि कर्मों में सुधार की सतत प्रक्रिया चलती रहे। कर्मों में सुधार के माध्यम से ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है।
सम्यक समाधि
अगर ऊपर बताये गए सिद्दांतों में सम्यकता रही तो मन से मौत का डर समाप्त हो जायेगा। तब मृत्यु जीवन का एक क्षण मात्र होगा। यही निर्वाण की प्राप्ति है।
अष्टागिंक मार्ग को व्यवहार में लाने के लिए, बुद्ध ने दस नैतिक उपदेश दिए हैं, जिनमें से पाँच केंद्रीय हैं, जिनपर बल दिया गया है और पाँच ऐसे हैं, जिनपर अधिक बल नहीं दिया गया।
ये नियम इस प्रकार हैं:
(1) किसी की जान मत लो।
(2) चोरी मत करो।
(3) व्यभिचार न करो।
(4) झूठ मत बोलो
(5) मादक पदार्थों का सेवन न करो।
(6) नियत समय को छोड़कर भोजन न करो।
(7) खेल-कूद और गाने-बजाने से बचो।
(8) फूल, सुगंध आदि से दूर रहो।
(9) अच्छे और मुलायम बिस्तर पर सोने से बचो।
(10) सोना-चांदी अपने पास न रखो।
यही अष्टागिंक मार्ग और दस नैतिक उपदेश बौद्ध धर्म की संपूर्ण नैतिक व्यवस्था के आधार हैं। बुद्ध ने जीविका और सामाजिकता के बारे में अपने अनुयायियों को जो भी निर्देश दिए, उनके आधार “आत्म-विनाश” और “संसार त्याग” है। क्योंकि इसका गंतव्य “निर्वाण” है और इसे आत्म-विनाश के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करने का विधान किया है। उदाहरण के लिए, दाढ़ी, मूंछ और सिर के बालों को नोचना ताकि सुंदरता का घमंड धूल में मिल जाए, हमेशा खड़े रहना, कांटों या कीलों के बिस्तर पर लेटना, हमेशा एक ही ओर सोना और शरीर पर धूल लगाना और इसी तरह के अन्य कार्य जो शरीर को कष्ट देते हैं और आत्मा को दुखी करते हैं और भावना को अमान्य कर देते हैं! इनके अलावा, बुद्ध ने जीने के सामान्य तरीक़ों के बारे में भी इसी तरह के आदेश दिए हैं। यहां उन सभी का विवरण देना बहुत कठिन है क्योंकि वे कई खंडों पर आधारित हैं, लेकिन कुछ को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है:
चार चीज़ें, जिनसे बचने पर बहुत ज़ोर दिया गया है, वे हैं: (1) स्त्री और पुरुष का नैसर्गिक संबंध। इसमें वैध और अवैघ का कोई अंतर नहीं। (2) चोरी – चाहे घास के एक तिनके की भी। (3) जानबूझकर किसी भी जीवित प्राणी की हत्या, यहाँ तक कि छोटे से छोटे कीड़े की भी। (4) अपने आप को एक असाधारण स्थिति का श्रेय देना।
धार्मिक जीवन अपनाने के बाद व्यक्ति को नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें कूड़े पर पड़े चीथड़े या कब्रिस्तान से मुर्दों के कफ़न ले कर लपेटना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के चीथड़े भी एक समय में तीन से अधिक नहीं होने चाहिए।
बौद्ध धर्म की परम्पराओं में यह प्रसंग प्रसिद्ध है कि जब अरवेला के मुखिया की पुत्री की मृत्यु हो गई और उसे पास के एक श्मशान में दफ़नाया गया, तो एक दिन बुद्ध ने उसकी कब्र खोली, उसका कफ़न निकाला और पास के एक तालाब में ले गया। जाकर उसे धोकर अपने हाथों से कुर्ते की तरह सी कर पहन लिया।
जीवनयापन के लिए कोई पेशा न करे, एक लकड़ी का भिक्षापात्र ले और चुपचाप भीख माँगता फिरे। यह भिक्षादान बौद्ध धर्म में सबसे शुद्ध आजीविका है। स्वयं बुद्ध अपने विहार से प्रतिदिन भिक्षा माँगने जाते थे। इसलिए वे अपने अनुयायियों को भिक्षु और स्वयं को महा भिक्षु कहते हैं, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा भिखारी।
आवास के लिए घर नहीं बनाना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए और पेड़ों की छाया में आश्रय लेना चाहिए। बीमार हो तो किसी भी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए, मूत्र का घोल इसके लिए पर्याप्त औषधि है।
अपने शरीर को साफ़ रखने की कोशिश भी न करें, पखवाड़े में एक बार नहाने की अनुमति है।
अपने पास रुपये-पैसे एक़दम न रखे। व्यापार, लेन-देन, क्रय-विक्रय तथा वे सभी कार्य जिनमें चाँदी और सोने का प्रयोग होता हो, से पूरी तरह बचे।
अच्छा बिस्तर कभी न रखे, एक मोटा झोठा कम्बल रखना चाहिए और उस कम्बल को कम से कम छ: वर्षों तक चलाना चाहिए।
बौद्ध धर्म की वास्तविक कमज़ोरी
यह उस संपूर्ण नैतिक व्यवस्था का सार है, जिसका एक अंश अहिंसा की शिक्षा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ही उच्च नैतिक निर्देश हैं। यह अनुचित होगा अगर हम गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई पवित्रता और शुद्धता की शिक्षा की प्रशंसा न करें, जिसका उन्होंने स्वयं अपने गौरवशाली जीवन में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन आंशिक रूप से बहुत सी खूबियां रखने के बावजूद यह सारा सिस्टम शुरू से अंत तक बुनियादी तौर पर ग़लत है। यह एक मिथ्या विश्वास पर आधारित है। मानव जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण ग़लत है। उन्होंने एक ग़लत स्थान से मनुष्य और उसके जीवन पर दृष्टि डाली है। एक ग़लत गंतव्य को मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ठहराया है, और उस तक पहुँचने के लिए एक ग़लत रास्ता सुझाया है। गौतम बुद्ध वास्तव में दुनिया में होने वाली घटनाओं और परिवर्तनों और जीवन की क्रांति और विकास से चकित हैं। वे उनके असली कारण को समझने की कोशिश नहीं करते। उनकी गहराइयों में उतरकर सत्य का पता नहीं लगाते। न साहस से उनका सामना करके किसी उच्च आदर्श की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। बल्कि वे उनका छिछला अध्ययन करते हैं और सरसरी नज़र डाल कर इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि मानव जीवन व्यर्थ है, संसार की सारी व्यवस्था निरर्थक है। इसमें जो क्रांति और परिवर्तन चल रहा है, उसका उद्देश्य मनुष्य को पीड़ा देने और कष्ट पहुँचाने के सिवा कुछ नहीं है। मनुष्य की बुद्धि, विवेक, भावना, चेतना, इच्छाएँ और शारीरिक शक्तियाँ जो भी प्राप्त हैं, वे उसे पीड़ित करने के लिए हैं और इसका कोई बेहतर उपयोग नहीं है। दुनिया की दौलत, इसकी संस्कृति, इसकी राजनीति, इसका शासन, इसका उद्योग और व्यापार, इसके सभी व्यवसाय बेकार हैं। ये सब संपर्क के फंदे हैं जो बार-बार मनुष्य को जीवन की ओर खींचते हैं और उसे पुनर्जन्म के सतत चक्र में बांधे रखते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य का और कोई कार्य नहीं है सिवाय इसके कि वह स्वयं को छोड़कर सभी बाहरी संबंधों से कट जाए और स्वयं को भी सभी प्रकार के आनंद और सुखों से वंचित करके कष्टों से ग्रसित कर ले। स्वयं को उस हद तक मिटा दे कि वह “होने” और “अस्तित्व” के बंधन से छूट कर “असितित्वहीनता” और “शून्यता” की सीमा में चला जाए।
अब यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति संसार के कष्टों से डरकर स्वयं ही संसार को त्याग देता है, वह स्वयं को सभी सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों से अलग कर लेता है, और केवल अपनी मुक्ति की चिंता में लग जाता है। और उस मोक्ष या शून्यता तक पहुँचने के लिए भी ऐसा रास्ता अपनाता है जो दुनिया के भीतर से नहीं, बल्कि बाहर-बाहर से जाता है। उससे अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने साथी मनुष्यों के कल्याण के लिए किसी बहादुरी भरे प्रयास या किसी छोटे से भी त्याग की अपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती। उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने मन-मस्तिष्क की शक्ति और अपने भौतिक और आध्यात्मिक संसाधनों के साथ समाज के विकास और सुधार के कार्य में भाग लेगा। दृढ़ संकल्प के साथ, क्रूरता और आक्रामकता, विद्रोह और बिगाड़, शोषण और उत्पीड़ण, पथभ्रष्टता और विचलन से बहादुरी के साथ संघर्ष कर के विश्व में न्याय, शान्ति का झंडा ऊंचा करेगा और प्राकृतिक कारणों से प्रत्येक कार्य में मनुष्य को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका साहसपूर्वक सामना करेगा।
यह संघर्ष, यह व्यावहारिक गतिविधियां, यह आत्म-बलिदान और वीरता, युद्ध के मैदान की ये कठिनाइयां, ये तीरों और तलवारों के घाव, ये राजनीति और नेतृत्व के बोझल उत्तरदायित्व तो वही वहन कर सकता है, जो इस संसार को कर्मभूमि मानता है। जिसके समक्ष जीवन का एक उच्च आदर्श, और एक उच्च उद्देश्य है। जो ख़ुद को एक महत्वपूर्ण सेवा में लगा हुआ और एक उच्चतम सत्ता के प्रति जवाबदेह समझता है, और जो मानता है कि इस दुनिया में वह जितना अधिक सत्कर्म करेगा, उतना ही अधिक उसे भविष्य, अनन्त जीवन में पुरस्कृत किया जाएगा। मगर जो बेचारा पहले ही अपने जीवन से हताश है, अपने कर्मों के परिणामों से निराश है, अपने आस-पास की कठिनाइयों से हार गया है, दुनिया की हर दुर्घटना से डर कर, हर मुसीबत से भयभीत होकर, हर क्रांति से आशंकित होकर, अस्तित्वहीनता की शरण ले रहा है, उस कायर, और कमज़ोर इरादों वाले व्यक्ति से कब उम्मीद की जा सकती है कि वह ज़िम्मेदारियों के इस भारी बोझ को उठाएगा और अपने आप को संघर्ष, राजनीति और नेतृत्व की कठिनाइयों में डालेगा। उसने तो पहले ही संसार के बखेरों को त्याग कर मृत्यु और अनन्त मृत्यु को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। फिर उसे क्या पड़ी है कि वह तलवार खींचकर कर्मक्षेत्र में निकल जाए और इस संसार के संचालन में अपना समय नष्ट करे, जिसके जीवन को वह व्यर्थ समझता है और जिसकी समस्त गतिविधियों को वह व्यर्थ और निष्फल समझता है।
अत: बौद्ध धर्म, जो अहिंसा में विश्वास करता है, इसलिए नहीं कि वह दुनिया और उसके मामलों की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है और फिर भी युद्ध और रक्तपात को अनावश्यक मानता है। बल्कि वास्तव में उसका कारण यह है कि उसका दुनिया और उसके मामलों से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह युद्ध और संघर्ष से भी दूर रहता है। उसने अहिंसा को इसलिए अपनाया है, कि संन्यास और संसार त्याग के जीवन में तलवार का कोई कार्य नहीं है, और उस लक्ष्य तक पहुँचने में उससे कोई मदद नहीं मिलती है जो बौद्ध संन्यासी का अंतिम लक्ष्य है।
बौद्ध अनुयायियों के जीवन पर अहिंसा का प्रभाव
बौद्ध धर्म की शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि वह विश्व में किसी शक्तिशाली सभ्यता की स्थापना नहीं कर सका। इसने कभी इतनी ताक़त विकसित नहीं की कि किसी सभ्यता को पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर सके। वह जिन देशों में पहुँचा वहाँ के नैतिक जीवन में नकारात्मक परिवर्तन लाने में अवश्य ही सफल रहा, परन्तु वह वहाँ की राजनीतिक शैली और सांस्कृतिक व्यवस्था को बदलकर एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हो सका और न ही उसने इसकी कोशिश की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे दुनिया में बहुत प्रचार मिला। मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व में, जितनी उन्नति उसने हासिल की उतनी कोई और हासिल नहीं कर सका। बड़ी मानव आबादी ने इसे स्वीकार किया। आज भी दुनिया में किसी भी अन्य धर्म की तुलना में इसके अधिक अनुयायी हैं। लेकिन इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से किसी राष्ट्र के जीवन में कोई बड़ी क्रांति आई हो या उसने दुनिया में कोई बड़ा कारनामा किया हो। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जहाँ भी उसे किसी शक्तिशाली सभ्यता का सामना करना पड़ा, उसकी करारी हार हुई। भारत, जो उसकी जन्मस्थली है, लम्बे समय तक यहां उसका घेरा बना रहा। पहली शताब्दी ईस्वी में लगभग पूरा देश इसका अनुयायी था, तीसरी शताब्दी ईस्वी में भी तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, चौथी शताब्दी में जब फाह्यान भारत आया था, तब भी यह धर्म यहाँ प्रचलित था, परन्तु उसके बाद जब ब्राह्मण धर्म ने अपनी करवट बदली, तो तीन शताब्दियों के भीतर बौद्ध धर्म को उसके लिए मैदान ख़ाली करना पड़ा और उनका नाम इस देश से इस तरह मिटा दिया गया कि आज बौद्धों की आबादी कुछ लाख से ज़्यादा नहीं है। David T.W. Rhys ने अपनी किताब Budhhist India में इस धर्म के पतन के कारणों की विवेचना करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणवाद के अनुयायियों ने इसे तलवार से नहीं मिटाया। अगर इस ऐतिहासिक शोध को स्वीकार कर लिया जाए तो यह बौद्ध धर्म की दुर्बलता का और भी प्रबल प्रमाण है। तलवार के बल से विलुप्त होना केवल भौतिक शक्ति की कमी को इंगित करता है, लेकिन तलवार के बिना एक शांतिपूर्ण मुक़ाबले में नष्ट हो जाना एक खुला तर्क है कि यह धर्म आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से ब्राह्मणवादी धर्म की तुलना में बहुत कमज़ोर था।
इसी प्रकार अफगानिस्तान में अशोक के प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म को बहुत प्रसार मिला और दूसरी शताब्दी ईस्वी में काबुल का राजा मिनांडर (या मलिंडा) स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, (स्मिथ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पृ225) लेकिन जब इस्लाम की शक्तिशाली सभ्यता द्वारा उसे चुनौती दी गई, तो वह एक क्षण भी नहीं ठहर सका। चीन में उसे जो भी स्थायित्व प्राप्त हुआ, वह केवल ताओवाद की सहायता का परिणाम था, अन्यथा कन्फ्यूशियस के धर्म ने तो उसे समाप्त ही कर दिया था। (हैकमैन, बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में, पृ. 83)
जापान में भी उसे शिंतो धर्म से बहुत कुछ लेकर मेल समझौता करना पड़ा, यहां तक कि उसके मुक़ाबले में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी बुनियादी मान्यताओं को भी बदलना पड़ा। (वही पीपी. 90-91)
बाक़ी रहे अन्य देश जैसे सीलोन, बर्मा, तिब्बत आदि, तो वहां उसका प्रतिरोध करने वाली कोई शक्तिशाली सभ्यता ही नहीं थी, इसलिए उसने आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इतिहास गवाह है कि उसने किसी भी युग में इन देशों में सभ्यता की भावना को नहीं जगाया। जैसे पहले वे निर्जीव और गतिहीन थे, वैसे ही वे बौद्ध काल में भी रहे।
इसके अलावा, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बौद्ध धर्म ने कभी शासन का सामना करने और समाज की भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने का साहस नहीं किया। बौद्ध धर्म में राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बौद्ध धर्म सत्ता में भाग लेने या उसे बदलने के बजाय, सभी परिस्थितियों में आज्ञाकारिता का आदेश देता है, चाहे वह शासक दमनकारी क्रूर हो या न्यायप्रिय और कल्याणकारी।(Vinaya Texts, Part l, P.301) इतना ही नहीं उसने शैतानी ताक़त के आगे ऐसी लाचारी और क्रूरता के सामने सहनशीलता की ऐसी सीख दी है कि उसका कोई अनुयायी कठोर से कठोर अत्याचार और क्रूरता पर भी उफ़ नहीं कर सकता। उसका कहना है कि इंसान को इस जीवन में जितने भी दुख झेलने पड़ते हैं वह उसके पहले जीवन में किए गए पापों का परिणाम है। इसलिए जब कोई शत्रु किसी पर अत्याचार करे तो उसे समझना चाहिए कि यह अत्याचारी दोषी नहीं है बल्कि मैं स्वयं दोषी हूं, मैंने पिछले जन्म में ऐसा ही गुनाह किया होगा जिसके लिए मुझे यह सज़ा मिल रही है। (Buddha and His Religion, P. 150-151) यह धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म के अनुयायियों में बदले की भावना को ठंडा कर देता है और एक ऐसी निष्क्रिय स्थिति बनाता है कि वे हर अपमान और हर क्रूरता को सहर्ष सहन कर लेते हैं।
ज़ाहिर है, एक दमनकारी शासन के लिए इससे ज़्यादा वांछनीय कुछ नहीं हो सकता। ऐसा धर्म उसके लिए ख़तरा होने के बजाय, स्थिरता का स्रोत होता है। ऐसी मान्यताओं में विश्वास रखने वाली प्रजा को संतोषपूर्वक सभी प्रकार के क्रूर क़ानूनों और दमनकारी आदेशों के अधीन किया जा सकता है। करों और रिश्वतों द्वारा हर तरह से लूटा जा सकता है। उसके जीवन और संपत्ति और सम्मान और प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह से हमला किया जा सकता है। उसे अत्याचारी शासकों की शैतानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से उपयोग किया जा सकता है। यही वजह है कि बौद्ध धर्म को शासकों से इतनी कम प्रतिस्पर्धा मिली है, बल्कि अधिकांश देशों में शासकों ने इसका विरोध करने के बजाय उत्साहपूर्वक इसका समर्थन किया है। मगध में जैसे ही बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हुआ, मगध के राजा बिम्बिसार ने उसे हाथों-हाथ लिया और उस धर्म के समर्थन में एक शिलालेख प्रकाशित किया।(Vinaya Texts, Part l, P. 136-197) उसका बाद उनके पुत्र अजातशत्रु, भी बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक रहा। कोसाल के राजा पासनादि (अग्निदत्त) ने स्वयं उन्हें अपने देश आने का निमंत्रण दिया और उनका धर्म स्वीकार कर लिया और उनसे संबंध बढ़ाने के लिए, शाक्य परिवार की कन्या से विवाह किया। (Buddhist India, P. 10-11) इसके अतिरिक्त परम्पराओं से ज्ञात होता है कि अवन्ति तथा एक अन्य महाजनपद के राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं समर्थक बन गए।(Buddhist India, P. 16)
इस काल के बाद तीसरी शताब्दी ई.पू. में हम देखते हैं कि अशोक ने इस धर्म का संरक्षण किया और अपने राजकीय संसाधनों का प्रयोग करके न केवल भारत और उसके पास पड़ोस में बल्कि दूर-दराज़ के देशों में भी इसका प्रचार-प्रसार किया। फिर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क ने उत्साहपूर्वक इस धर्म का समर्थन किया। उसके बाद तीसरी शताब्दी ई. में विक्रर्मादित्य प्रथम ने ब्राह्मणवाद का अनुयायी होने के बावजूद बौद्ध धर्म को संरक्षण और मजबूती प्रदान की। फिर सातवीं शताब्दी में उसे एक शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त हुआ और उसने उसका इतना प्रबल समर्थन किया कि ब्राह्मणवादी संप्रदाय ने हर्षवर्धन की हत्या की साज़िश रचनी शुरू कर दी।(Smith Early History of India, P.349)
भारत के बाहर तिब्बत और मंगोलिया में कुबलई खान ने इस धर्म के प्रचार-प्रसार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि वह इसे राजनीतिक कारणों से अपने राज्य के लिए उपयोगी समझता था। (Buddhism as a Religion, P. 73-74) चीन में, राजा मिंग टी ने स्वयं उसके प्रचारकों को अपने यहां आमंत्रित किया और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। (Buddhism as a Religion, P. 177) उसके बाद भी कई राजा उसका समर्थन और सहयोग करते रहे। यही हाल अन्य देशों का भी है, जिनकी स्थिति इतिहास को खंगालकर भली-भांति जानी जा सकती है।
अत: बौद्ध धर्म को विश्व में जो प्रसार प्राप्त हुआ और कालांतर के बावजूद अधिकांश देशों में शताब्दियों तक जीवित रहा, इसलिए नहीं कि उसकी एक शक्तिशाली संस्कृति थी या उसकी जीवन शक्ति बहुत प्रबल थी, बल्कि इसलिए कि वह अत्याचारी शासनों के आगे सदैव सर झुकाता रहा। उसने अत्याचार के सामने खड़े होने का कभी साहस नहीं किया। अत्याचारी शासकों के शासन से मानवता को मुक्त कराने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। इसलिए, शासकों ने हमेशा इसका समर्थन किया और उसके अस्तित्व को अपने वर्चस्व के लिए उपयोगी माना।
इस संक्षिप्त टिप्पणी से यह देखा जा सकता है कि युद्ध के मामले में इस्लाम और बौद्ध धर्म के बीच किस तरह का अंतर है। इस्लाम के अनुसार, मनुष्य को दुनिया में एक महान उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है और उसकी मुक्ति इस दुनिया को अच्छी तरह बरतने में है। इसलिए, वह मनुष्य को उन सभी कार्यों को अपनाने का आदेश देता है जो उसके नैतिक और भौतिक कल्याण और सांसारिक जीवन के सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं। इसके विपरीत बौद्ध धर्म की दृष्टि में मानव जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और उसका उद्धार केवल इसी में है कि संसार और उसके सभी संबंधों, यहाँ तक कि अपने आप से भी विमुख हो जाए। इसलिए, वह उसे किसी ऐसे व्यावहारिक प्रयास या मानसिक रुचि की अनुमति नहीं देता है जो उसे दुनिया की किसी भी चीज़ के संपर्क में रखे। अब पवित्र बुद्धि स्वयं निर्णय कर सकती है कि मानवता के लिए इस्लाम का जिहाद अधिक उपयोगी है या बौद्ध धर्म की अहिंसा।
(4) ईसाइयत
दूसरा धर्म जिसका युद्ध के मामले में इस्लाम से बुनियादी मतभेद है, वह ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म से आशय वास्तव में वह धर्म नहीं है, जिसकी शिक्षा हज़रत ईसा ने दी थी, बल्कि वह धर्म है जिसे हज़रत ईसा से जोड़ा जाता है। हमारे पास इस तथ्य के लिए मज़बूत तर्क हैं कि हज़रत ईसा ने इस ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी थी, बल्कि वे तो उसी इस्लाम को लेकर आए जो उनके पहले के सभी पैग़म्बर ले कर आए थे और उनके बाद हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ले कर आए। आगे चलकर हम इनमें से कुछ तर्कों का वर्णन भी करेंगे। हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम यहां ईसाई धर्म के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, वह वास्तव में ईसा मसीह के धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उस धर्म से संबंधित है जो ईसा मसीह के नाम पर बनाया गया है।
यहूदी धर्म की तरह, ईसाई धर्म के बारे में भी हमारी जानकारी का एकमात्र स्रोत वह एक किताब है जिसे समस्त ईसाईजगत अपने धर्म की मूलभूत पुस्तक के रूप में स्वीकार करता है, और वह है बाइबल। लेकिन इससे पहले कि हम उससे वास्तविक समस्या के बारे में पूछें, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आज वह जिस हालत में मौजूद है, उससे वर्तमान ईसाई धर्म की मान्यताएँ ही हमें ज्ञात हो सकती हैं, अन्यथा यह प्रश्न कि मूल रूप से हज़रत ईसा की शिक्षा क्या थी, इससे हल नहीं होता। चूँकि आगे की चर्चा को समझने के लिए इस मामले को ध्यान में रखना आवश्यक है, इसलिए आइए आगे बढ़ने से पहले बाइबल की किताबों की ऐतिहासिक स्थिति पर एक नज़र डाल लीजिए।
ईसाइयत के स्रोतों की जांच
आज हम जिस संग्रह को बाइबल कहते हैं, वह वास्तव में चार प्रमुख धर्मग्रंथों, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से मिलकर बना है। लेकिन इनमें से कोई भी शास्त्र हज़रत ईसा का नहीं है। पवित्र क़ुरआन में जिस प्रकार अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर अल्लाह की ओर से अवतरित होने वाली सभी आयतें और सूरतें अपने मूल रूप में जमा हैं, उस प्रकार किसी भी किताब में वे प्रकाशनाएं हमें नहीं मिलती हैं, जो कि हज़रत ईसा पर अवतरित हुई थीं। साथ ही, हम उन उपदेशों और सलाहों को स्वयं यीशु के शब्दों में कहीं भी नहीं पाते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के दौरान पैग़म्बर के रूप में विभिन्न अवसरों पर कहे थे। ये शास्त्र जो हम तक पहुँचे हैं, न तो अल्लाह के शब्द हैं और न ही ईसा मसीह के, बल्कि ये वास्तव में ईसा मसीह के शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें उन लोगों ने अपने ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार, ईसा मसीह के हालात और उनकी शिक्षाओं को एकत्र किया है।
लेकिन इन किताबों की बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं कि इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहली किताब को ईसा मसीह के शिष्य मत्ती या मैथ्यू से जोड़ा जाता है, लेकिन यह इतिहास से प्रमाणित है कि वह मैथ्यू की लिखी हुई नहीं है। मैथ्यू की मूल किताब, जिसका नाम Logia (लोजिया) था, विलुप्त हो चुकी है। जिस किताब को मैथ्यू से जोड़ा जाता है, उसका लेखक कोई गुमनाम व्यक्ति था, जिसने अन्य किताबों के साथ लोजिया से भी फ़ायदा उठाया था। इसमें स्वयं मैथ्यू का उल्लेख इस तरह किया गया है, जैसे किसी अंजान व्यक्ति का किया जाता है।
मैथ्यू, अध्याय 9, पद 9 में लिखा है:
“यीशु वहां से चले गए और टैक्स बूथ पर मैथ्यू नाम के एक आदमी को देखा।”
स्पष्ट है कि है, लेखक स्वयं अपना उल्लेख इस तरह नहीं कर सकता था।
इसके अध्ययन से पता चलता है कि यह काफ़ी हद तक मरकुस के बाइबल से लिया गया है। क्योंकि इसके 1028 छंदों में से 470 ठीक वैसे ही हैं जैसे मरकुस के बाइबल में पाए जाते हैं। हालाँकि, अगर इसका लेखक अगर मैथ्यू होता, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की किताब का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो न तो यीशु का शिष्य था और न ही कभी यीशु से मिला था। ईसाई विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ ईसा के 41 वर्ष बाद यानी 70 ईस्वी में लिखा गया था और कुछ का मानना है कि इसे 90 ईस्वी में लिखा गया था।
दूसरी किताब को मरकुस से जोड़ा जाता है, और यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि मरकुस ख़ुद ही उसका लेखक है, लेकिन यह सिद्ध है कि वह ईसा मसीह से कभी नहीं मिला और न उनका शिष्य बना। वह वास्तव में सेंट पीटर्स का शिष्य था और उससे जो कुछ सुनता था उसे ग्रीक भाषा में लिख लेता था। इस कारण से, ईसाई लेखक आमतौर पर उसे “पीटर्स का दुभाषिया” के रूप में संदर्भित करते हैं। माना जाता है कि यह किताब 63 ईस्वी और 70 ईस्वी के बीच लिखी गई है।
तीसरी किताब को लूका से जोड़ा जाता है और यह बिल्कुल प्रमाणित है कि लूका ने कभी भी ईसा मसीह को नहीं देखा और न कभी उनसे लाभ उठाया। वह सेंट पॉल का शिष्य था, हमेशा उनकी संगति में रहा, और उसने अपने बाइबल में सेंट पॉल के विचारों ही की व्याख्या की है। अतः स्वयं सेंट पॉल उसके बाइबल को अपना बाइबल कहता है। लेकिन यह सिद्ध है कि सेंट पॉल स्वयं ईसा मसीह के सान्निध्य से वंचित था और ईसाई परम्परा के अनुसार उसने सूली की घटना के 6 वर्ष बाद इस धर्म में प्रवेश किया। इसलिए, लूका और ईसा मसीह के बीच की एक कड़ी पूरी तरह से गायब है। लूका के बाइबल के लिखे जाने की तिथि भी निर्धारित नहीं है। कुछ कहते हैं कि यह 57 ईस्वी में लिखा गया था और कुछ कहते हैं कि यह 74 ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन हार्निक, मैक-गिफर्ट और प्लुमर जैसे शोधकर्ताओं की राय है कि यह 80 ईस्वी से पहले नहीं लिखा गया था।
चौथी किताब, जिसे जॉन (युहन्ना) का बाइबल कहा जाता है, आधुनिक शोध के अनुसार, प्रसिद्ध जॉन द एपोस्टल द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि जॉन नामक एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। यह किताब ईसा मसीह के बहुत बाद, 90 ईस्वी में या उसके भी बाद लिखी गई है। हार्निक इस अवधि को 110 ईस्वी तक बढ़ा देते हैं।
स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी किताब ईसा मसीह तक नहीं पहुँचती है और इनके प्रमाणों पर भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। लेकिन गहन पड़ताल से इन किताबों की दस्तावेज़ी स्थिति और भी संदिग्ध हो जाती है। सच्चाई यह है कि ये किताबें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के मामले में क़ुरआन तो दूर हदीस के सबसे कमज़ोर संग्रह के बराबर भी नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका वह स्थान है, जो हमारे यहां मौलूद शरीफ़ का है।
पहली बात यह कि चारों बाइबलों के विवरण भिन्न हैं। यहाँ तक कि ‘पहाड़ी के उपदेश’ को भी, जो कि मसीही शिक्षाओं की नींव है, मैथ्यू, मरकुस और लूका ने अलग-अलग और परस्पर विरोधी ठंग से उल्लिखित किया है।
दूसरी बात यह कि चारों बाइबलों में उनके लेखकों के विचार और मत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। मैथ्यू के संबोधित यहूदी प्रतीत होते हैं, और वह उन्हें संबोधित करता प्रतीत होता है। मारकुस के संबोधित रोमन हैं और वह उन्हें इज़राइलवाद से अवगत कराना चाहता है। लूका सेंट पॉल का अभिभाषक है और अन्य शिष्यों के ख़िलाफ़ उसके दावों का समर्थन करना चाहता है। युहन्ना उन दार्शनिक विचारों से प्रभावित प्रतीत होता है, जो ईसाइयों के बीच पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में फैल गए थे। इस प्रकार इन चार बाइबलों के बीच शाब्दिक अंतर से अधिक मौलिक अंतर हो गया है।
तीसरी बात यह कि सभी बाइबलें यूनानी भाषा में लिखी गई हैं, हालांकि ईसा मसीह और उनके सभी शिष्यों की भाषा सीरियाई थी। भाषा की भिन्नता के कारण विचारों की व्याख्या में भिन्नता होना स्वाभाविक है।
चौथी बात यह कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से पहले बाइबलों को लिखित रूप में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 150 ईस्वी तक, आम धारणा यह थी कि मौखिक उल्लेख लिखित की तुलना में अधिक उपयोगी है। दूसरी शताब्दी के अंत में लेखन का विचार पैदा हुआ, किन्तु उस काल की रचनाएँ प्रामाणिक नहीं मानी जाती हैं। न्यु टेस्टामेंट का पहला प्रामाणिक पाठ कार्थेज की परिषद में स्वीकार किया गया, जो 397 ईस्वी में आयोजित हुई थी।
पाँचवीं बात यह कि, बाइबलों की सबसे पुरानी पांडुलिपि जो वर्तमान दुनिया में मौजूद है, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य की है। दूसरी प्रति 5वीं शताब्दी की है और तीसरी अधुरी प्रति जो कि पोप के पुस्तकालय में है, चौथी शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं है। इसलिए यह कहना कठिन है कि वर्तमान बाइबलें कुछ हद तक उन बाइबलों के अनुरूप हैं जो पहली तीन शताब्दियों में प्रचलित थीं।
छठी बात यह कि बाइबलों को, कभी भी पूरा याद करने का प्रयास नहीं किया गया। इनका प्रकाशन प्रारंभ में अर्थपूर्ण वर्णन पर निर्भर था, जिसमें स्मृति की विकृति और कथाकारों के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव स्वाभाविक है। बाद में, जब लेखन प्रक्रिया शुरू हुई, तो वह नक़ल करने वालों की दया-दृष्टि पर थी। नक़ल करते समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आसान था कि वह उसमें जो कुछ अपनी मान्यताओं के विरुद्ध पाए उसे हटा दे और जो कमी पाए उसे जोड़ दे।
ऊपर की पूरी बहस इन किताबों से ली गई है : Dumellow Commentary on the Holy Bible, Y.K.Cheeyne, Encyclopaedia Biblica Millman, History of Christainity.
ये वे कारण हैं जिनके आधार पर हम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि हमें चार बाइबलों में ईसा की मूल शिक्षा मिलती है। इसलिए, अगले पृष्ठों में ईसाई धर्म के बारे में जो कहा जाएगा, वह उस धर्म के बारे में नहीं होगा जिसकी शिक्षा ईसा मसीह ने दी थी, बल्कि यह उस ईसाई धर्म के बारे में होगा जिसे आज की ईसाई दुनिया मानती है।
“प्रेम” की शिक्षा
बाइबल के अध्ययन से पता चलता है कि ईसाई धर्म युद्ध के सख़्त ख़िलाफ़ है, चाहे युद्ध सत्य के लिए हो या असत्य के लिए। ईसा के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा आदेश यह है कि “गॉड से प्रेम करने के बाद अपने पड़ोसी से प्रेम करो।” (मत्ती 22:39) और इस प्रेम के साथ यह भी अनिवार्य है कि “तू अपने भाई पर क्रोध न कर” (मत्ती 5:22)। लेकिन वे केवल प्यार करने और ग़ुस्सा न करने पर ही नहीं रुकते, बल्कि स्पष्ट शब्दों में एक सच्चे ईसाई को निर्देश देते हैं कि वह अत्याचार और उद्दंडता के सामने अपना सिर झुका दे और दूसरों की रक्षा करना तो परे, ख़ुद अपने अधिकार की रक्षा भी न करे। उनकी शीक्षा का क्रीम पहाड़ी का उपदेश है, जिसपर ईसाई नैतिकता की नींव स्थापित है, उसमें वे कहते हैं:
तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत।
परन्तु मैं तुम से यह कहता हूं, कि बुरे का सामना न करना; परन्तु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उस की ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे; और जो तुझ से उधार लेना चाहे, उस से मुंह न मोड़॥ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था; कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। परन्तु मैं तुम से यह कहता हूं, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिये प्रार्थना करो। (मत्ती 5:38-44)
“परन्तु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम से बैर करें, उन का भला करो। जो तुम्हें श्राप दें, उन को आशीष दो: जो तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन ले, उस से न मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं।” (लूका 6:27-32)
यह शिक्षा ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत है और इसका उद्देश्य उसके अपने शब्दों से स्पष्ट है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि एक सच्चा ईसाई जो स्वर्गीय पिता (Heavenly Father) की तरह सिद्ध होना चाहता है (मत्ती 5:47) और जिसका मिशन “परमप्रधान की सन्तान” होना है (लूका 6:35) किसी स्थिति में अत्याचार और दमन का मुक़ाबला शक्ति से नहीं करना चाहिए। बल्कि दुष्टों और दुराचारियों के सामने अपने अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए।
ईसाइयत में नैतिकता का दर्शन
इस शिक्षा के गुण और दोष को तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है जब तक कि ईसाई धर्म की आत्मा को अच्छी तरह से न समझ लिया जाए।
जिस रूप में ईसाइयत हमारे पास आई है, उस पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह वास्तव में संन्यास, मठवाद और त्याग का धर्म है। इसमें मनुष्य के सभ्य जीवन के लिए कोई संविधान, कोई क़ानून, कोई संहिता नहीं बनाई गई है। यह किसी व्यक्ति को यह नहीं बताता कि उसपर उसके परिवार, उसके समाज, उसके राष्ट्र, और उसके पालनहार के क्या अधिकार हैं और उन्हें चुकाने का सही तरीक़ा क्या है। अल्लाह ने मनुष्य को जो भौतिक संसाधन और मानसिक और शारीरिक शक्ति दी है, उसका उपयोग क्या है और उसे इन चीज़ों का उपयोग कैसे करना चाहिए। व्यावहारिक जीवन के इन विषयों पर वह कोई चर्चा नहीं करता। इसके ध्यान का केंद्र केवल एक प्रश्न है और वह यह है कि मनुष्य “स्वर्गीय राज्य” में कैसे प्रवेश कर सकता है। यही एक प्रश्न समस्त ईसाई नैतिकता की धुरी है। मसीह ने जो शिक्षा दी है, उसका उद्देश्य मानव समुदाय को उसी लक्ष्य तक ले जाने के लिए तैयार करना है।
लेकिन ईसाई धर्म की दृष्टि में “स्वर्गीय राज्य” ज़मीन के राज्य के विकसित रूप का नाम नहीं है। यह इन दोनों के बीच बीज और फल के संबंध को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि इन दोनों के बीच विरोधाभास की मान्यता रखता है। इसके अनुसार, सांसारिक राज्य और स्वर्ग का राज्य दो अलग-अलग चीज़ें हैं, और दोनों परस्पर नहीं रह सकते, जैसे कि आग और पानी परसपर नहीं रह सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का विलोम समझने का परिणाम यह है कि दह “स्वर्गीय राज्य” को प्राप्त करने का रास्ता भी सांसारिक राज्य के रास्ते से पूरी तरह से अलग अपनाता है। ऐसी सभी चीज़ जो सांसारिक राज्य के उपकरण में शामिल है, स्वर्गीय राज्य के उपकरण से बाहर रखी गयी है, और न केवल बाहर रखी गयी है, बल्कि उसका अस्तित्व मनुष्य को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोकने वाला माना जाता है। यही कारण है कि ईसाई धर्म मनुष्य से क़दम दर क़दम आग्रह करता है कि अगर वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे ज़मीन के राज्य के सामानों को पूर्णत: त्याग देना चाहिए, और अगर वह उन का त्याग नहीं कर सकता है, तो स्वर्ग के राज्य की आशा न रखे। उसी सिद्धांत पर, वह मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में संसार त्याग की शिक्षा देता है और सभ्यता व संस्कृति से पूर्णत: अलग करके इंसान को संन्यासी बना देना चाहता है। इसे समझाने के लिए, मसीह के कुछ आदेशों को उद्धृत करना पर्याप्त है:
“यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहिनों बरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।” (लूका, 14:26)
“क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुम से कहता हूं; नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से दो तीन से। पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा; मां बेटी से, और बेटी मां से, सास बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी॥ ” (लूका, 12:51-53)
“तुम ने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में न तो सोना, और न रूपा, और न तांबा रखना। मार्ग के लिये न झोली रखो, न दो कुरते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मज़दूर को उसका भोजन मिलना चाहिए।” (मत्ती, 10:8-10) ).
“हे छोटे झुण्ड, मत डर; क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो; और अपने लिये ऐसे बटुए बनाओ, जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिस के निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता।” (लूका 12:32-33)
“यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है; तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा; और आकर मेरे पीछे हो ले।” (मत्ती 19:21)
ईसा मसीह ने यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति को दिया था, जो मैथ्यू, मारकुस और ल्यूक के सर्वसम्मत बयान के अनुसार, हत्या, व्यभिचार, चोरी और झूठ बोलने से परहेज़ करता था, अपने माता-पिता की सेवा करता था और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करता था। मसीह ने उससे कहा कि तू पूर्ण तब होगा जब अपना सारा माल बेचकर दान कर देगा।
“ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। ” (मत्ती, 19:23-24)
“अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो; जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं।” (मत्ती, 6:19)।
“इसलिये यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा॥” (मत्ती, 6:14-15)
“इसलिये मैं तुम से कहता हूं, कि अपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे? और क्या पीएंगे? और न अपने शरीर के लिये कि क्या पहिनेंगे? क्या प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो! वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं; तौभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को खिलाता है; क्या तुम उन से अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है, जो चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिये क्यों चिन्ता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो, कि वै कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं, न कातते हैं। तौभी मैं तुम से कहता हूं, कि सुलैमान भी, अपने सारे विभव में उन में से किसी के समान वस्त्र पहिने हुए न था। इसलिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहिनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम को वह क्योंकर न पहिनाएगा? इसलिये तुम चिन्ता करके यह न कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पीएंगे, या क्या पहिनेंगे?” (मत्ती, 6:25-31)
इन कथनों से यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म जिस तरह से मानव समुदाय को स्वर्गीय राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है, उसका सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। सभी जानते हैं कि पारिवारिक बंधन सभ्य जीवन की नींव होते हैं। समुदाय से व्यक्ति का प्रारम्भिक सम्बन्ध अपने सम्बन्धियों के माध्यम से ही होता है, उनके आपसी सम्बन्धों से सामूहिक निकाय का निर्माण होता है और वास्तव में यही मनुष्य के लिए नैतिकता की सर्वोत्तम पाठशाला भी है। लेकिन “मसीह” की कुल्हाड़ी की पहली चोट इसी नींव पर पड़ती है और वह सबसे पहले उस बंधन को काट देता है जो मनुष्य को समाज से जोड़े हुए है। पहली चीज़ जो मनुष्य को दुनिया को बरतने और उसके मामलों में भाग लेने के लिए कार्रवाई करने पर मजबूर करती है, वह है पेट भरने और शरीर ढंकने की चिंता। लेकिन “मसीह” इस प्रारंभिक प्रेरक को ही मार देना चाहते है., ताकि मनुष्य दुनिया में हवा के पक्षियों और जंगल के वृक्षों की तरह रहे। मानव आराम और व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए धन अर्जित करना अनिवार्य है। लेकिन “मसीह” के अनुसार आध्यात्मिक विकास और स्वर्गीय राज्य की प्राप्ति के लिए इसे छोड़ना ज़रूरी है। दुनिया में शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना राजनीति, दंड और प्रतिशोध के क़ानून पर निर्भर करती है, परन्तु “मसीह” कहते हैं कि स्वर्गीय पिता उस समय तक तुम्हारे गुनाह क्षमा नहीं करेगा, जब तक कर्म-प्रतिफल के इस पूरे क़ानून को लपेट कर रख न दिया जाए। “मसीह” के अनुसार धर्म वास्तव में संसार त्याग का नाम है। वह जो दुनिया और इसके संसाधनों का त्याग नहीं करता, सामाजिक बंधनों को नहीं तोड़ता, सांसारिक गतिविधियों से ख़ुद को अलग नहीं करता है और पूर्ण संन्यासी जीवन नहीं अपनाता है, उसके लिए स्वर्ग के राज्य में कोई स्थान नहीं है। मनुष्य एक ही समय में इन दोनों राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता। लोक और परलोक इन दोनों को पा लेना उस के लिए असंभव है। ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें हैं, इसलिए जिसे एक की चाहत हो उसे दूसरे की मांग को छोड़ना होगा।”
“मसीह” की इस शिक्षा को स्वयं ईसाई विद्वान जिस रंग में प्रस्तुत करते हैं, उस का आकलन करने के लिए रेवरेंड डुमेलो द्वारा की गई बाइबल की व्याख्या के कुछ अंशों को यहां उद्धृत करना पर्याप्त है। यह व्याख्या 40 से अधिक ईसाई विद्वानों की मदद से तैयार की गई है और यह बाइबिल की सबसे अच्छी व्याख्याओं में से एक है। इस में “मसीह की शिक्षा” नामक एक स्थायी लेख है जिसमें लिखा है:
“The General Type of Christian Character. Christianity has approved a type of character in most respects the very opposite of that which is approved by the world: instead of pride, humility; instead of standing upon one's rights, submission to wrong; instead of ambition, contentment. Gentleness, meekness, patience, sympathy, the power of rejoicing in tribulation, and of extracting pleasure from pain, are the gifts of Christianity to the world. The Christian ideal is sometimes depreciated as lacking in manliness and courage, but in truth it requires much more manliness to be humble than to be proud, much more courage to turn the cheek to the smiter than to smite again. Another great note of the Christian character is truthfulness and sincerity. According to Christ a Christian man's word should be as good as his oath. This is the meaning of the paradoxical saying, 'Swear not at all,' etc. (Mt. 5:34). But perhaps the best general description of a Christian man's character is to say that he is a single-minded man. He cannot have one foot in the world and the other in the Church, he cannot serve God and mammon. He must have one main purpose in life to which all others are to be subordinated: ' Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you' (Mt.6:33).
Christ regarded wealth as the great means by which the world binds men to its service. Detachment from wealth, therefore, is a necessary preliminary to being a Christian.” (Commentary on the Holy Bible, Dumellow. P. LXXX)
“ईसाई चरित्र का सामान्य प्रकार। ईसाइयत ने एक ऐसे प्रकार के चरित्र को मंजूरी दी है जो कि दुनिया द्वारा स्वीकृत चरित्र के बिल्कुल विपरीत है: आत्मसम्मान के बजाय विनम्रता; अपने अधिकारों पर जमे रहने के बजाय, बुराई के आगे सर झुकाना; महत्वाकांक्षा के बजाय संतोष। विनम्रता, शालीनता, धैर्य, सहानुभूति, पीड़ा में आनन्दित होने की शक्ति, और दर्द से सुख निकालने की शक्ति, दुनिया के लिए ईसाई धर्म के उपहार हैं। ईसाई आदर्श को कभी-कभी साहस की कमी के रूप में आंका जाता है, लेकिन वास्तव में गर्व करने की तुलना में विनम्र होने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता है, थप्पड़ मारने वाले को पलट कर मारने की तुलना में उसके सामने दूसरा गाल बढ़ाने के लिए अधिक साहस की आवश्यकता है। ईसाई चरित्र की एक और महान विशेषता सच्चाई और ईमानदारी है। जीसस के अनुसार एक ईसाई व्यक्ति का वचन उसकी शपथ के समान होना चाहिए। 'Swear not at all,' का यही अर्थ है, (मत्ती 5:34)। लेकिन शायद एक ईसाई व्यक्ति के चरित्र का सबसे अच्छा सामान्य विवरण यह कहना है कि वह एकाग्र व्यक्ति है। उसका एक पैर दुनिया में और दूसरा चर्च (परलोक) में नहीं हो सकता, वह एक ही समय में गॉड और धन, दोनों की सेवा नहीं कर सकता। उसके जीवन में एक मुख्य उद्देश्य हो और शेष सारे उद्देश्य उसके अधीन होने चाहिए: इसलिये पहिले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।' (मत्ती 6:33)। जीसस ने धन को महान साधन माना जिसके द्वारा दुनिया मनुष्यों को अपनी सेवा में बांधती है। इसलिए, धन से वैराग्य एक ईसाई होने के लिए एक आवश्यक शर्त है।" (पवित्र बाइबिल पर टिप्पणी, डूमेलो, पृ. LXXX)
ईसाई नैतिकता का मुख्य दोष
अब यह सर्वविदित है कि ईसाई धर्म में प्रेम, क्षमा और विनम्रता की जो शिक्षा दी गई है, दह एक ऐसी नैतिक व्यवस्था के घटकों में से है, जो संसार त्याग के आधार पर स्थापित की गई है । चूंकि ईसाइयत ने परलोक में मुक्ति का रास्ता सांसारिक कल्याण के मार्ग से अलग चुना है, इसलिए वह दुनिया के मामलों को दुनियादारी के लिए छोड़ देती है और अपने भक्तों को लेकर अलग हो जाती है ताकि एकांत में बैठकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने की तैयारी करे, ऐसे धर्म में युद्ध न होने का मतलब यह नहीं है कि वह दुनिया और उसके मामलों की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है और उसे पूरा करने के लिए शक्ति के प्रयोग को आवश्यक नहीं समझता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि चूंकि उसे दुनिया और उसके मामलों से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वह युद्ध और रक्तपात से भी इनकार करता है। वह यह नहीं कहता कि बुराई को मिटाने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह कहता है कि बुराई को मिटाने की ही ज़रूरत नहीं है। वह यह नहीं कहता कि उद्दंडता का विनाश युद्ध के बिना भी हो सकता है, बल्कि वह कहता है कि उद्दंडता के विनाश की चिन्ता करना ही व्यर्थ है, उससे लड़ने के स्थान पर उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। वह यह नहीं कहता कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सत्य का संरक्षण बिना रक्तपात के भी संभव है, बल्कि वह कहता है कि सत्य की रक्षा ही मत करो, अत्याचारी तुम्हारा अधिकार छीने तो उसे छीन लेने दो। वह यह नहीं कहता कि अपराधियों को बिना हिंसा के भी दंड दिया जा सकता है और पीड़ितों का बदला बिना बलप्रयोग के भी लिया जा सकता है, बल्कि, वह कहता है कि दंड और प्रतिशोध को ही छोड़ दो और कोई “सात बार नहीं, सत्तर बार भी अपराध करे, तो उसे क्षमा कर दो।”
दूसरे शब्दों में, दुनिया में शांति स्थापित करना, इसे बुराई और दुष्टता से सुरक्षित रखना, इसमें न्याय और निष्पक्षता की स्थापना करना और मानवता को अत्याचार और अत्याचार के वर्चस्व से मुक्त कराना, ये सभी ईसाई धर्म के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसने अपने लिए अधीनता और दमन का जीवन चुन लिया है। इसलिए अगर वह युद्ध के ख़िलाफ़ है और सत्य-असत्य के अंतर के बिना युद्ध को बुरी चीज़ मानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे जीवन के लिए यही रवैया अधिक उपयुक्त है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या अपमान और निष्क्रियता की यह शिक्षा मनुष्य के लिए एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक क़ानून बन सकती है? इसका जवाब ईसाइयत स्वयं अपने मुंह से दे रही है। जब यह सिद्ध हो चुका है कि युद्ध से अलग रहने का आदेश स्वयं कोई स्थायी क़ानून नहीं है, बल्कि संन्यास और संसार त्याग के व्यापक क़ानून के प्रावधानों में से एक है, तो इससे यह निष्कर्श स्वयं निकलता है कि युद्ध से अलग रहने का नियम तभी लागू किया जा सकता है जब संसार त्याग का पूरा क़ानून लागू हो। ईसाइयत स्वयं यह नहीं कहती है कि आपको दुनिया का प्रबंधन अपने हाथों में लेना चाहिए, लेकिन लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसकी अपनी शिक्षा के अनुसार, एक व्यक्ति इस विनम्रतापूर्ण निष्क्रिय जीवन को तभी अपना सकता है जब वह दुनिया को त्याग दे और उसकी विभिन्न सांस्कृतिक ज़िम्मेदारियों से अलग हो जाए। इन सभी ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करना और इन्हों पूरा करना, यह दृष्टिकोण न तो संभव है और न ही स्वयं मसीह द्वारा अभिप्रेत है। अब अगर इसे सार्वभौम नियम घोषित कर दिया जाए तो पूरी मानव जाति को अनिवार्य रूप से सभ्यता से विमुख होना पड़ेगा।
अगर मनुष्य का गंतव्य “स्वर्ग का राज्य” हो और यह भी मान लिया जाए कि सांसारिक जीवन के सारे मामले उस राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि उस मंज़िल तक पहुँचने के लिए मानव जाति उस बाधक चीज़ से बचे और संन्यासी जीवन अपनाकर इच्छाओं के दमन और अनुशासन में लग जाए। लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसा होना असंभव है। पूरी दुनिया एक ही समय में अपना कारोबार बंद नहीं कर सकती और वह आजीविका की चिंता छोड़ कर “हवा के पक्षियों” और “जंगली पेड़ों” की तरह नहीं रह सकती। व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य सभी गतिविधियों को त्याग कर ठहराव और आलस्य की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती। यह सरकार और उसके प्रशासन को छोड़ कर मठों में नहीं बैठ सकती। और अगर किसी तरह वह ऐसा कर भी ले उसके लिए असम्भव होगा कि वह उस सम्मान और प्रतिष्ठा को पा ले जो अल्लाह ने उसे अन्य प्राणियों की तुलना में प्रदान किया है, बल्कि सच तो यह है कि यह जीवित भी नहीं रह सकती। इसलिए, यह कहना पूरी तरह से अनुचित है कि ईसाई धर्म का नैतिक क़ानून समस्त मानव जाति के लिए एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक क़ानून है, क्योंकि एक सार्वभौमिक और सर्वकालिक क़ानून केवल वही हो सकता है जिसका सभी स्थितियों में दुनिया के सभी निवासियों द्वारा पालन किया जा सके।
फिर यह क़ानून किसी एक पूरे समुदाय पर भी लागू नहीं हो सकता। अगर एक राष्ट्र या समुदाय समग्र रूप से उसके आदेशों को स्वीकार करता है और “स्वर्ग के राज्य” में प्रवेश करने के लिए उनके सभी निर्देशों का पालन करता है, तो उसे पहले अपनी सरकार की व्यवस्था को निलंबित करना पड़ेगा। अपनी सेना और पुलिस को भंग करना होगा। अपनी सीमाओं की सुरक्षा और किलों की रखवाली छोड़नी होगी। फिर जब एक पड़ोसी राष्ट्र मैदान को ख़ाली देखकर हमला करेगा, तो ईसाई शिक्षा के अनुसार, यह कथित अच्छा राष्ट्र बुराई के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा, बल्कि एक गाल के साथ दूसरा गाल भी आगे बढ़ा देगा। तब वह अपना सारा धन, अपना व्यापार, अपनी दुकानें, यहां तक कि अपने घरों की संपत्ति भी छोड़ देगा, क्योंकि “स्वर्ग के राज्य में धनी” प्रवेश नहीं कर सकता। और आदेश यह है कि “फिर अपनी सारी दौलत बेच कर दान में दे दो।” “फिर वह जीवनयापन के लिए काम-धंधा नहीं करेगा, अपने व्यवसायों को बंद कर, उद्योग, शिल्प, सेवा को छोड़कर सारा समुदाय मठों में जा बैठेगा। क्योंकि “आप गॉड और धन, दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते।” और मसीह का आदेश है कि “अपने जीवन के बारे में चिंता मत करो।” अन्त में उसके पास जीविका का एकमात्र साधन भूमि को जोतना तथा अपने भोजन के लिए अनाज उत्पन्न करना ही रह जाता है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि मसीह ने कहा, “आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न ही काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। इस प्रकार, ईसा मसीह के अनुयायी अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना धन, अपना उद्योग और व्यापार उन विदेशी आक्रमणकारियों को समर्पित कर देंगे और पूरा देश उनका ग़ुलाम बन जाएगा। फिर वे अत्याचार करेंगे और ये उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें प्रताड़ित करेंगे और ये उनके लिए गॉड से क्षमा याचना करेंगे। वे इनके आत्मसम्मान को कुचलेंगे इनकी इज़्ज़त पर हमले करेंगे और ये उनकी प्रतिषठा बढ़ाने की दुआएं मांगेंगे। ईसाई दृष्टिकोण से यह उनकी नैतिकता की पूर्णता है जिसके बाद कुछ भी उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, मगर बुद्धि और विवेक की दृष्टि से यह ऐसा अपमान और पतन की चरम सीमा है, जिसकी प्राप्ति को एक बुद्धिमान व्यक्ति आत्महत्या के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द से व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं नहीं समझता कि आख़िर वह स्वर्गीय राज्य है किस तरह का, जिसमें ऐसे निकम्मे, लज्जाहीन और चरित्रहीन लोगों की मांग और खपत है। हालाँकि, जहाँ तक इस दुनिया का संबंध है, यह स्पष्ट है कि इस दुनिया में कोई भी राष्ट्र ईसाई धर्म के नैतिक क़ानून को अपने जीवन का क़ानून नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति अपने अस्तित्व की रक्षा करने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस क़ानून की एक-एक घारा को तोड़ने पर मजबूर कर देगी। और व्यवहारिक तौर पर उसके उल्लंघन के बाद केवल आस्था के लिए उस पर विश्वास रखना बेमानी होगा।
अब तीसरा मामला यह है कि इसे पूरे राष्ट्र के लिए भी एक सार्वभौमिक क़ानून नहीं माना जाए, बल्कि इसे एक विशेष समूह के लिए विशिष्ट माना जाए, जैसा कि स्वयं “मसीह” के विनिर्देशों से पता चलता है। यह स्थिति निश्चित रूप से संभव है। अगर मानव समुदाय के अलग-अलग समूह अपनी अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करते रहें। कोई व्यापार करता रहे, कोई उद्योग में लगा हो, कोई कृषि करता हो, कोई राजनीतिक कार्यों में लगा हो और इस प्रकार सभ्यता का कारख़ाना सुचारू रूप से चलता रहे। तो यह संभव है कि समाज अपने एक छोटे हिस्से को “हवा के पक्षियों और जंगली लिली-वृक्षों” की तरह निष्क्रिय और व्यर्थ जीवन बिताने के लिए छोड़ दे। और उसके कुछ सदस्य ईसाई नैतिकता की उस परम पूर्णता तक पहुँचने के प्रयास में लगे रहें, जो संसाधनों को त्याग करने, संबंधों को तोड़ने, स्वाभिमान को कुचलने, आत्म-विनाश और आत्म-अस्वीकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस क़ानून को एक विशेष समूह तक सीमित मानने के लिए, और दूसरी ओर इसे मुक्ति के सच्चे और एकमात्र साधन के रूप में पहचानने का अर्थ यह है कि हम मोक्ष या स्वर्ग के राज्य पर भिक्षुओं और संन्यासियों के एक छोटे समूह के एकाधिकार को मान्यता देते हैं और यह मान लेते हैं कि उस छोटे से “राज्य” के संकीर्ण दायरे में मानवजाति के आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग सभ्य व्यवस्था चलाते हैं, सरकार और राजनीति की योजना बनाते हैं, देश और देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और विभिन्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग-अलग व्यवसाय संभाले हुए हैं, उनके लिए इस “राज्य” के द्वार बंद हैं, क्योंकि ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दुनिया और धर्म, दोनों में पैर नहीं रख सकता है। स्वर्गीय राज्य का द्वार केवल तभी खुल सकता है जब वे दुनिया छोड़कर मसीह द्वारा सिखाए गए धार्मिक जीवन को अपनाते हैं। इस तरह, एक छोटे समूह को “स्वर्गीय पिता के राज्य” में प्रवेश करने का अवसर मिलता है और अल्लाह की बाक़ी सारी सृष्टि उससे वंचित कर दी जाती है। यहां तक कि उन्हें भी वहां सिथान नहीं मिल सकता, जो लोग संसार में अच्छाई और पवित्रता से रहते हैं। वे हत्या नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, चोरी और झूठ बोलने से बचते हैं, अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी सारी संपत्ति बेचकर उसे दान में नहीं दे देते।
इस मत को सही मानने का अर्थ है कि हम पुन: पहली स्थिति की ओर लौट रहे हैं। अगर यह स्वीकार किया जाता है कि “स्वर्गीय साम्राज्य” अर्थात मोक्ष के लक्ष्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ईसाई धर्म का नैतिक नियम है, और जो उसका पालन नहीं करता है वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता है, तो निश्चित रूप से इसे भी स्वीकार करना होगा कि यह समस्त मानव जाति के लिए एक सार्वभौमिक क़ानून है, क्योंकि मोक्ष हर इंसान की नियति है और किसी मार्ग को उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीक़ा घोषित करने का मतलब है कि यह सभी मनुष्यों के लिए बना है और हर कोई उससे बंधा हुआ है। लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त मानव जाति के लिए इस मार्ग पर एकत्रित होना और एक स्वर में आगे बढ़ना तार्किक और व्यवहारिक रूप से असम्भव है। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार ईसाई धर्म द्वारा बनाया गया क़ानून सार्वभौमिक और सर्वकालिक नहीं है, साथ ही वह भी मुक्ति का न्यायसंगत और एकमात्र साधन भी नहीं है। सार्वभौमिक, सर्वकालिक और मोक्ष का एकमात्र साधन तो वही विधान हो सकता है, जिसपर शासक, शासक रहते हुए, व्यापारी, व्यापारी रहते हुए, किसान, किसान रहते हुए और पर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िम्मेदारी अदा करते हुए, पालन कर सकता हो। जिसके अनुपालन में किसी भी इंसान के लिए दुर्गम कठिनाइयां, असहनीय खतरे और अंतहीन पीड़ाएं न हों। जो विधान ऐसा नहीं है, वह न तो सत्य का सीधा मार्ग है, न मुक्ति का एकमात्र साधन है, न ही प्रकृति का एक सच्चा नियम है।
इस शंका को ख़ुद ईसाइयों ने भी महसूस किया, और इसलिए यह नियम पैदा किया गया कि मुक्ति के लिए ईसाई धर्म का पूरी तरह पालन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मसीह ने स्वयं सूली पर चढ़कर अपने सभी अनुयायियों के लिए प्रायश्चित कर दिया है, और मसीह उन सभी लोगों के उद्धारकर्ता हैं जो उन पर आस्था रखते हैं। लेकिन इस नियम की कमज़ोरी स्पष्ट है। इसे स्वीकार करने के बाद ईसाई धर्म की नैतिक संहिता की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। अगर प्रायश्चित का यह सिद्धांत सही है, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति हत्या कर सकता है, चोरी कर सकता है और व्यभिचार कर सकता है, अपने पड़ोसी को सता सकता है और अनुचित ढंग से धन जमा कर सकता है, फिर भी “स्वर्गीय राज्य” में प्रवेश कर सकता है, शर्त केवल यह है कि वह मसीह में आस्था रखता हो। इस स्थिति में वे सारी नैतिक शिक्षाएं व्यर्थ हो जाती हैं, जो मसीह ने अपने धर्मोपदेशों में दी हैं। बल्कि मसीह का अपना कथन भी ग़लत हो जाता है कि इन कर्मों के साथ कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर मसीह का यह कथन सत्य है, तो प्रायश्चित की मान्यता निश्चित रूप से असत्य है। ये दोनों मान्यताएं एक साथ नहीं चल सकती हैं। यह किसी तरह संभव नहीं है कि ये दोनों किसी एक ही धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा हों।
लेकिन हम इस बिंदु पर भी नहीं रुक सकते। हमें एक क़दम और आगे जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ईसाई धर्म का नैतिक क़ानून अपने वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह से प्रकृति के विपरीत है। यह वास्तव में नैतिक सद्गुणों की एक झूठी अवधारणा का परिणाम है, जिसमें कुछ सद्गुणों पर असंतुलित ढंग से अत्यधिक बल दिया जाता है और अन्य सद्गुणों को अनावश्यक रूप से निलंबित कर दिया जाता है, जिससे मानवता पंगु हो कर रह जाती है। मानवीय नैतिकता के जिन गुणों पर वह ज़ोर देता है, वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। क्या कोई विनम्रता, लाचारी, क्षमा, सहनशीलता और धैर्य के गुणों को नकार सकता है? लेकिन केवल इन्हीं गुणों के आधार पर मानव जीवन का निर्माण करना उचित नहीं है। अगर दुनिया से बुराई और दुष्टता पूरी तरह से मिट जाए, धरती पर इंसानों की जगह देवदूत बसने लगें और शैतान अपने कूल को लेकर दूसरे ग्रह पर चला जाए, तो संभव है कि इंसान अपनी शारीरिक ताक़त और तीव्रता का इस्तेमाल किए बिना अपने अधिकारों, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। लेकिन जब दुनिया में अच्छाई के साथ-साथ बुराई भी है और मानव स्वभाव से दुष्टता के गुण मिट नहीं गए हैं, भलाई के गुणों को पराजित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छाई को निहत्था छोड़ देना और अल्लाह द्वारा दी गई शक्तियों को उसकी रक्षा के लिए उपयोग में न लाना, न केवल आत्महत्या है बल्कि बुराई का अप्रत्यक्ष सहयोग भी है। सच तो यह है कि अत्याचारियों को जानबूझकर अन्याय और अत्याचार करने का मौक़ा देना और उद्दंड लोगों को जानबूझकर बिगाड़ फैलाने की खुली छूट देना कोई भलाई नहीं है। हम इसे कमज़ोरी कह सकते हैं, कायरता कह सकते हैं और साहस की कमी कह सकते हैं, लेकिन इसे भलाई और परोपकार तो कदापि नहीं कह सकते। सदाचार वास्तव में सुधार का दूसरा नाम है और यह प्रेम और क्रोध के एक मध्यम संयोजन से पैदा होता है। अगर क्षमा, धैर्य और सुख से बुराई का सुधार किया जा सकता है, तो उस से किया जाना चाहिए, और अगर प्रेम की ये शक्तियाँ सफल नहीं होती हैं, तो राजनीति, दंड और प्रतिशोध की शक्तियों का उपयोग करना ज़रूरी है। क्योंकि वास्तविक लक्ष्य सुधार है, और यह मनुष्य का दायित्व है कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता की सीमा तक हर तरीक़े का उपयोग करे। तरीक़ों के बीच भेदभाव करना और किसी एक तरीक़े पर इस हद तक ज़ोर देना कि वह सुधार के बजाय बिगाड़ को और बढ़ावा दे, न तो भलाई है और न ही समझदारी।
ईसाई धर्म का यह विचार कि धर्म का मूल सिद्धांत “प्रेम” है और उसके सिवा सभी मानवीय भावनाएँ और नैतिक लक्षण अमान्य हैं, उन्हें मिटाकर ही धर्म विकसित हो सकता है, वास्तव में एक मिथ्या कल्पना पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों की नज़र इस तथ्य तक नहीं पहुंच सकी कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया है। उन्होंने समझ लिया कि क्रोध, वासना और आत्म-प्रेम जैसी अन्य भावनाएं मनुष्य में बिना किसी ज़रूरत के पैदा हो गई हैं और मानव जीवन में साहस और आत्मतुष्टि, साहस और वीरता, चातुर्य और राजनीति, न्याय आदि का कोई उपयोग नहीं है। हालाँकि, यह सोच पूरी तरह से ग़लत है। मनुष्य में जितने गुण, शक्तियां और भावनाएँ जमा हैं, उन सभी का अपना उपयोग और उद्देश्य है। जिस प्रकार मनुष्य का कोई अंग, यहां तक कि एक रोम भी बेकार नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य का कोई मानसिक और शारीरिक बल, कोई बाहरी और आंतरिक गुण, और कोई भावना भी बेकार नहीं है। सृष्टि के रचयिता ने इसे बिना किसी समीचीनता के नहीं बनाया है। अगर ये शक्तियाँ ग़लत रूप में प्रकट होती हैं और ग़लत रास्ता अपनाती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपने आप में ग़लत और बुरी हैं, बल्कि इसका कारण केवल यह है कि मनुष्य ने उनके सही उपयोग को नहीं समझा है और यह कि उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई है कि वह उनके उचित उपयोग की दिशा में उसका मार्गदर्शन कर सके।
उदाहरण के लिए कामवासना एक ऐसा भाव है जिसके कारण मनुष्य ने इतने पाप किए हैं, जितने किसी दूसरी भावना के तहत न किए होंगे। मगर इस आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता, कि इसे पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इसी कर्म पर मानव जाति का अस्तित्व निर्भर है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो दुनिया में अनगिनत झगड़े और अत्याचार का कारण बना है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह विशुद्ध बुराई है और इसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि यह दुनिया में शांति और व्यवस्था की गारंटी है, अन्यथा बुराई और दुष्टता की ताक़तें शांति और व्यवस्था को नष्ट कर दें।
ठीक ऐसा ही हाल उन भावों और गुणों का है जिन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। उनमें जहां बहुत सी भलाइयां हैं, वहीं बहुत सी बुराइयां भी हैं। अगर बहादुरी हद से आगे बढ़ जाए तो वह अहंकार और मूर्खता की हद तक पहुंच जाती है। दूरदर्शिता अगर अतिशयोक्ति का पक्ष ले ले तो वह कायरता और नपुंसकता बन जाती है। दया अगर अपनी मर्यादा में न रहे तो वह अपराधों और पापों की सहायक बन जाती है। अगर उदारता हद से ज़्यादा हो जाए तो यह फ़िज़ूलख़र्ची का रूप ले लेती है। अगर मितव्ययिता हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वह कंजूसी में बदल जाती है। अगर प्रेम अपनी सीमा में न रहे तो वह मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। सहानुभूति का अगर अनुचित प्रयोग किया जाए तो वह बुरे कार्यों में दुस्साहस पैदा करती है। विनम्रता और सहनशीलता अगर अपने स्थान पर न हो तो आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाता है। कुल मिलाकर यह कि मनुष्य को जो भी भावनाएं और ताक़तें दी गई हैं उनके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। उनमें से एक पहलू को देख कर न तो उनकी अच्छाई या बुराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और न ही उनमें से किसी के परित्याग और किसी को अपनाए जाने का आदेश दिया जा सकता है। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि मनुष्य के लिए केवल हाथ, पैर, हृदय और मन ही उपयोगी हैं, आँख, नाक, पेट और कलेजे की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, केवल सुनने और चखने की क्षमता काफ़ी है, देखने और सूंघने की क्षमता की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी तरह हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एक इंसान में केवल प्यार और दया, क्षमा और सहनशीलता, लाचारी और विनम्रता, की ही ज़रूरत है, घृणा और क्रोध, बहादुरी और साहस, आत्म-संयम और अभिमान की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य सभी शारीरिक शक्तियों के संयम पर निर्भर करता है, और जिस प्रकार मन का स्वास्थ्य तभी प्राप्त होता है जब सभी मानसिक बल आनुपातिक रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार नैतिकता की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब भावनाओं और इच्छाओं में संयम होता है। एक प्राकृतिक धर्म का कार्य इसी संयम की ओर मार्गदर्शन करना है, न कि किसी एक असंतुलन के जवाब में दूसरा असंतुलन और एक अति के जवाब में दूसरी अति पैदा कर देना।
ईसाई धर्म इस बड़ी सच्चाई को समझने में असमर्थ रहा है। इसलिए उसने मनुष्य को संसार-त्याग की शिक्षा दी और निश्चय कर दिया कि मनुष्य को केवल दीनता और अकर्मण्यता को ही अपने जीवन का नियम बना लेना चाहिए। लेकिन यह न तो नैतिक उत्कृष्टता का स्तर है और न ही मानवता की सेवा। बल्कि सच तो यह है कि यह मानवता पर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। जो लोग जीवन के इस तरीक़े को अपनाते हैं, एक ओर ख़ुद को उन वैध आनंदों और सुख-सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो अल्लाह ने उनके लिए बनाएं हैं, और दूसरी ओर, अपने अस्तित्व को बेकार कर देते हैं और मानव समुदाय के लिए अपनी सेवाओं को निलंबित कर देते हैं। ईसाई धर्म ने सांसारिक राज्य को स्वर्गीय राज्य से अलग कर दिया है। उसने गॉड और धन को दो विरोधी शक्तियाँ घोषित किया और सच्चे अनुयायियों को आदेश दिया है कि वे धन का परित्याग कर के गॉड के लिए एकाग्र हो जाएं और सांसारिक राज्य से विमुख होकर केवल स्वर्गीय राज्य के हो जाएं। इसका स्वाभाविक परिणाम तो यही हो सकता है कि सच्चे, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले, पवित्र और भले लोग दुनिया से अलग हो जाएँ और दुनिया के सारे मामले समाज के निकृष्ट वर्गों के हाथों में चले जाएँ, जो न अल्लाह से डरने वाले हों और न ही उनमें ईमानदारी पाई जाती हो। सत्ता पर दमनकारियों और अत्याचारियों का क़ब्ज़ा हो, व्यापार लालची और बेईमानी लोगों का हिस्सा बन जाए। उद्योग पर घोटालेबाज़ और जालसाज़ नियंत्रण पा लें और बुराई और बिगाड़ की ताक़तें समाज की पूरी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दें। जब अच्छे लोग जो समाज को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, अपने हाथ-पैर तोड़कर बैठ जाएंगे, निश्चित रूप से दुष्ट लोग सत्ता में आएंगे। उनके बुरे कर्मों की कम से कम आधी ज़िम्मेदारी उन भले लोगों पर अवश्य डाली जाएगी जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और कार्यक्षेत्र को दुष्ट लोगों के लिए ख़ाली छोड़ दिया।
मसीह के आह्वाण की वास्तविकता
इस बहस से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसाई धर्म में युद्ध, राजनीति और दंड के प्रावधानों का अभाव उसकी पूर्णता का प्रमाण नहीं है, बल्कि उसके दोष का प्रमाण है। ईसाई धर्म हमारे सामने जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह इतने अधिक दोषों से भरा हुआ है, कि उसके बताए हुए तरीक़े पर दुनिया का कोई समुदाय नहीं चल सकता है।
लेकिन ईसाई धर्म और उसके इतिहास के गहन अध्ययन से एक और तथ्य सामने आता है। जब हम ईसा मसीह की शिक्षाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें आस्था और नैतिकता की मोटी-मोटी बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई संविधान नहीं है, न ही कोई स्थायी आचार संहिता है, न ही अधिकारों और दायित्वों और लेन-देन के बारे में कोई निर्देश, यहां तक कि पूजा की कोई विधि भी निर्धारित नहीं है। ज़ाहिर है, ऐसा धर्म स्थायी धर्म नहीं हो सकता। आस्थाओं और कुछ नैतिक दिशानिर्देशों को सीखने के बाद, बहुत सी ऐसी चीज़ें बाक़ी रह जाती हैं, जिनके लिए एक धर्म के अनुयायियों को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। जिस धर्म में ये निर्देश मौजूद न हों, वह एक अलग धार्मिक व्यवस्था बनने में सक्षम नहीं हो पाता।
अब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या ईसा मसीह ने ऐसे अधूरे धर्म को स्थायी धर्म बनाया था। और क्या मसीह इस तथ्य से अनजान थे कि इस तरह के धर्म का पालन समस्त मानव जाति द्वारा तो क्या, किसी एक समुदाय द्वारा भी, हर स्थिति और हर युग में नहीं किया जा सकता है? ईसाई इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हैं। लेकिन जब हम ईसाई धर्म के इतिहास का अध्ययन करते हैं और उन परिस्थितियों को देखते हैं जिनमें यह पैदा हुआ था, और उन उद्देश्यों की जांच करते हैं जिनके लिए यह अस्तित्व में आया था, तो हमें एक अलग ही उत्तर मिलता है।
तथ्य यह है कि ईसाई धर्म स्वयं एक स्थायी धर्म नहीं था, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्मशास्त्र को पूरा करने और इसराईल की संतान के सुधार के लिए पैदा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का धर्मशास्त्र जिस ज़माने में भेजा गया था वह इसराईल की संतान की मानसिक बाल्यावस्था का ज़माना था। उनके पास किसी भी गहरी नैतिक शिक्षा को स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए, हज़रत मूसा ने उन्हें एक साधारण आस्था और नैतिकता की एक सरल आचार संहिता की शिक्षा देकर छोड़ दिया, जिसमें नैतिक गुणों, आध्यात्मिक शुद्धता और विश्वास की भावना का अभाव था। कुछ शताब्दियों तक बनी इस्राइल (इसराईल की संतान) उस क़ानून का पालन करते रहे, लेकिन बाद के समय में जब उनके मामलों का विस्तार हुआ, तो क़ानून में जो कमी रह गई थी, वह सामने आने लगी। धीरे-धीरे बनी इस्राइल की नैतिक स्थिति बिगड़ती गई और नैतिक बिगाड़ का भौतिक परिणाम राष्ट्रीय पतन के रूप में प्रकट हुआ। पहले उनकी एकता में फूट पड़ी, फिर बिखरे हुए घटक आपस में भिड़ने लगे और अंत में वे ग़ुलाम बना लिए गए, जिसने उन्हें पतन के गर्त में पहुँचा दिया।
(यहां फिर से, मैं पाठकों के सामने यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि यह पूरी बहस वर्तमान तोराह, बाइबल और इसराइली व ईसाई साहित्य और वर्तमान समय के ऐतिहासिक शोध पर आधारित है। क़ुरआन इस पूरे मामले को एक अलग ही रंग में पेश करता है।)
ईसा के जन्म से 738 वर्ष पूर्व अश्शूरियों (Assyrians) ने उन पर विजय प्राप्त की और दो शताब्दियों तक वे तथा बेबीलोन के लोग उन पर अत्याचार करते रहे। फिर 538 ई.पू. में ईरानी आए और 200 वर्षों तक उनका वर्चस्व रहा। उनके बाद, सिकंदर महान के नेतृत्व में यूनानियों ने उन्हें जीत लिया। (334-323 ईसा पूर्व) और सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र के टॉलेमी ने उसे अपनी सत्ता में मिला लिया। इस तरह, एक सदी तक बनी इसराईल यूनानियों की ग़ुलामी में रहे। फिर 198 ईसा पूर्व में, एक और अंय यूनानी राजवंश, सेलौकेडिया ने उन पर अपना शासन स्थापित कर लिया और उन्हें बलपूर्वक मूर्तिपूजा पर विवश किया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में, यहूदियों ने स्वतंत्रता की कुछ भावना महसूस की और विद्रोह किया और 141 ई.पू में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना की, जो लगभग 80 वर्षों तक चला। लेकिन उनकी नैतिकत स्थिति इस हद तक गिर चुकी थी कि उनका एकजुट रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए उनमें फूट पड़ गई और उन्होंने ख़ुद रोमनों को अपने देश आने का न्यौता दिया। ईसा के जन्म के 60 वर्ष पूर्व रोमनों ने फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया और जब ईसा मसीह ने आंखें खोलीं तो उनका पूरा देश रोमनों द्वारा ग़ुलाम बना लिया गया था। इस प्रकार आठ शताब्दियों तक बाबुल और अश्शूर के तारापूजकों, ईरान के अग्निपूजकों और यूनान और रोम के मूर्तिपूजकों के अधीन दास जीवन व्यतीत करने के कारण इसमें नैतिकता, प्रतिष्ठा, धर्मपरायणता और मानवता का कोई चिह्न शेष न रहा था।
बाइबिल में ही हमें यहूदियों के इस नैतिक और आध्यात्मिक पतन के कई विवरण मिलते हैं। 7 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बाबुलियों के प्रभाव में यरूशलेम के राजा मंसेसा ने पवित्र भूमि में जिन त्रुटियों की शुरुआत की उसका विवरण राजाओं-2 अध्याय 21 में इस तरह वर्णित है:
“उसने उन ऊँचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था, फिर बनाया, और इसराईल के राजा अहाब के समान बाल के लिये वेदियाँ और एक अशेरा बनवाई, और आकाश के सारे गणों को दण्डवत् और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियाँ बनाईं जिसके विषय यहोवा ने कहा था, "यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूँगा।" वरन् यहोवा के भवन के दोनों आँगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिये वेदियाँ बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया; और शुभ-अशुभ मुहूर्त्तों को मानता, और टोना करता, और ओझों और भूत सिद्धिवालों से व्यवहार करता था; उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, और जिनसे वह क्रोधित होता है।अशेरा की जो मूर्ति उसने ख़ुदवाई, उसको उसने उस भवन में स्थापित किया, जिसके विषय में यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान से कहा था, "इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इसराईल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूँगा।” (2 राजाओं, 21:3-7)
उस काल की नैतिक स्थिति का वर्णन पैग़म्बर होशे (782-741 ईसा पूर्व) ने इस प्रकार किया है:
“हे इस्राईलियों, यहोवा का वचन सुनो; इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करूणा और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहां शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता; वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और ख़ून ही ख़ून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव-जन्तुओं, और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे; और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी॥” (4:1-3)
740-701 ईसा पूर्व में, पैग़म्बर य़शायाह कहते हैं:
“तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय दु:ख से भरा है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाये गए, न बान्धे गए, न तेल लगा कर नरमाये गए हैं॥ तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं; तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं; वह परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ है।” (1:5-7)
“जो नगरी सती थी सो क्योंकर व्यभिचारिन हो गई! वह न्याय से भरी थी और उस में धर्म पाया जाता था, परन्तु अब उस में हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चान्दी घातु का मैल हो गई, तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते, और न विधवा का मुकद्दमा अपने पास आने देते हैं।” (1:21-23)
“उनकी जेवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाखमधु, ये सब पाए जाते हैं; परन्तु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते, और उसके हाथों के काम को नहीं देखते॥ इसलिये अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरूष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिये अधोलोक ने अत्यन्त लालसा कर के अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनन्द करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं।” (5:12-14)
“हाय उन पर जो दाखमधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस ले कर दुष्टों को निर्दोष, और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं! इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जल कर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल हो कर उड़ जाएंगे; क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना, और इसराईल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है।” (5:22-24)
उसी दौर के एक और नबी हज़रत मीका अलैहिस्सलाम कहते हैं:
“मैं ने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इसराईल के घराने के न्याइयों, सुनो! क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर, और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो, तुम, लोगों पर से उनकी खाल, और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो; वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते, और उनकी खाल उधेड़ते हो; तुम उनकी हड्डियों को हांड़ी में पकाने के लिये टुकड़े टुकड़े करते हो।” (3:2-3)
“ हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इसराईल के घराने के न्यायियो, हे न्याय से घृणा करने वालो और सब सीधी बातों की टेढ़ी-मेढ़ी करने वालो, यह बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या कर के और यरूशलेम को कुटिलता कर के दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले ले कर विचार करते, और याजक दाम ले ले कर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रूपये के लिये भावी कहते हैं; तौभी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिये कोई विपत्ति हम पर न आएगी।” (3:9-11)
बनी इसराईल के पैगम्बरों के इन कथनों से ज्ञात होता है कि उस ज़माने में यहूद्यों से धार्मिकता की वास्तविक भावना अर्थात् ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सदाचार और पवित्रता निकल चुकी थी। हरामख़ोरी, लालच, अत्याचार, निर्लज्जता और दुराचार ने पूरे समुदाय को घेर लिया था। उनके शासक अत्याचारी थे, उनके धर्मगुरु धोखेबाज़ थे, उनके नेता विश्वासघाती थे और उनकी प्रजा अपराध में लिप्त हो गई थी। उन्होंने घर्मग्रंथ के शब्दों और बाहरी रीति-रिवाजों को असली धर्म मान लिया था और उस आध्यात्मिक हक़ीक़त को भूल गए थे जो हर सच्चे धर्मग्रंथ के आदेशों का असली मंशा होता है। बनी इसराईल में दिन ब दिन बढ़ती इस गिरावट और पाखंड को देखते हुए ईसा से पहले भी बहुत से पैग़म्बर सुधार की कोशिश करते रहे थे। वह उन्हें उपदेशों द्वारा भूला हुआ पाठ याद दिलाते कि अल्लाह केवल जानवरों की क़ुरबानी और दुआओं से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि सच्चाई, दया, सहानुभूति और अच्छे व्यवहार से प्रसन्न होता है, और उनकी कृपा पाने के लिए क्षमा, प्रेम और अपनी इच्छाओं के बलिदान की ज़रूरत होती है। इसलिए बाइबल में हमें पैग़म्बरों के ऐसे उपदेश बहुतायत से मिलते हैं। यशायाह कहते हैं:
“ यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेलबलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं; मैं बछड़ों वा भेड़ के बच्चोंवा बकरों के लोहू से प्रसन्न नहीं होता॥ तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिये आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्नबलि फिर मत लाओ; धूप से मुझे घृणा है। नये चांद और विश्रामदिन का मानना, और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझ से सहा नहीं जाता। तुम्हारे नये चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं; वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उन को सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुम से मुंह फेर लूंगा; तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तौभी मैं तुम्हारी न सुनूंगा; क्योंकि तुम्हारे हाथ ख़ून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो: मेरी आंखों के साम्हने से अपने बुरे कामों को दूर करो; भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो; यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो; अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो॥ यहोवा कहता है, आओ, हम आपस में वादविवाद करें: तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तौभी वे हिम की नाईं उजले हो जाएंगे; और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तौभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी हो कर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे; और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे; यहोवा का यही वचन है॥” (1:11-20)
एक अन्य अवसर पर, पैग़म्बर यशायाह पूजा और कर्मों की आध्यात्मिक भावना और नैतिक उत्कृष्टता की शिक्षा इस प्रकार देते हैं:
“ सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उस से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाईं झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं, कि, अन्याय से बनाए हुए दासों, और अन्धेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन को छुड़ा लेना, और, सब जुओं को टूकड़े टूकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहिनाना, और अपने जातिभाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाईं चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा; तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा; तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यदि तू अन्धेर करना और उंगली मटकाना, और, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दु:खियों को सन्तुष्ट करे, तब अन्धियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अन्धकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा।” (58:4-10)
एक अन्य पैग़म्बर हज़रत मीका, उसी आध्यात्मिक शिक्षा को इस प्रकार नवीनीकृत करते हैं:
“मैं क्या ले कर यहोवा के सम्मुख आऊं, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के साम्हने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिये एक एक वर्ष के बछड़े ले कर उसके सम्मुख आऊं?
क्या यहोवा हज़ारों मेढ़ों से, वा तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित्त में अपने पहिलौठे को वा अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है; और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले?” (6:6-8)
ये शिक्षाएं सात शताब्दियों तक बहरे कानों से टकराकर वापस आती रही। इसराईलियों की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती गई। उनके बीच जड़ पकड़ चुके नैतिक बिगाड़ को दूर करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली सुधारक की ज़रूरत थी। इसलिए, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने हज़रत ईसा मसीह को भेजा और उन्होंने मीका और यशायाह के इस उपदेशों को नए उत्साह और एक नई भावना के साथ प्रस्तुत किया। पहले के पैगम्बरों की तरह ही, उनकी शिक्षा भी हज़रत मूसा के धर्मशास्त्र को निरस्त कर के उसके स्थान पर एक अलग धर्म स्थापित करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य केवल उस कमी को पूरा करना था, जो हज़रत मूसा के धर्मशास्त्र में रह गई थी। उस समय, यहूदी नैतिकता में धार्मिकता, ईमानदारी, विनम्रता, क्षमा, संतोष, अल्लाह का भय, दया, सहानुभूति और आत्म-बलिदान का बहुत अभाव था। वे अत्यधिक लालची, स्वार्थी आत्मकेंद्रित और संसारोनमुख हो गए थे। धर्मपरायणता की भावना, जो मानवता की आत्मा है, उनमें नहीं रह गई थी। इसलिए, मसीहा ने अपनी सारी ऊर्जा इन्हीं दोषों को दूर करने में लगा दी और मूल धर्मशास्त्र को बनाए रखते हुए, केवल उन चीज़ों को उस में जोड़ा जो समय के अनुसार आवश्यक थीं। इसलिए ईसाई धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि, वास्तव में, यह यहूदी धर्म का एक हिस्सा है, और अधिक सही शब्दों में, यह इसका पूरक है।
ठीक यही बात बाइबल में हज़रत ईसा मसीह द्वारा भी कही गयी है। कहते हैं :
“यह न समझो, कि मैं व्यवस्था था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा; परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि यदि तुम्हारी धामिर्कता शास्त्रियों और फरीसियों की धामिर्कता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे॥” (मत्ती, 5:17-20 और लूका, 16:17)
एक अन्य स्थान पर वे अपने अनुयायियों को आदेश देते है:
“तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसलिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिन को उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हें मनुष्यों के कन्धों पर रखते हैं; परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते।” (मत्ती, 23:1-4)
इन कथनों से पता चलता है कि ईसाई धर्म में हज़रत मूसा के धर्मग्रंथ के सभी आदेशों को रखा गया है और उनमें केवल पुण्य और धार्मिकता जोड़ी गई है।
ईसाइयत में युद्ध न होने का कारण
अब यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ईसाई धर्म में युद्ध, शांति, सरकार, राजनीति, दंड आदि से संबंधित सभी आदेश बाक़ी रखे गए थे, जिनका उल्लेख तोराह में किया गया था। ईसा मसीह का धर्म उनमें से किसी का भी इनकार नहीं करता था, यहां तक कि एक शब्द का भी नहीं। लेकिन ईसा मसीह ने उन आदेशों को लागू नहीं किया क्योंकि जिस युग में उनका जन्म हुआ था, उस युग में उन्हें लागू करने का कोई अवसर नहीं था।
ऊपर कहा जा चुका है कि ईसा के आगमन के समय, उनका देश सात से आठ सौ वर्षों से अन्य जातियों की ग़ुलामी में रहा था। उनके जन्म के केवल 60 साल पहले, रोमन सेना ने फ़िलिस्तीन पर आक्रमण किया था और उसे एक छोर से दूसरे छोर तक रौंदती चली गई थी। जिस समय मसीह ने अपनी आंखें खोलीं, उस समय उनका पूरा देश रोमियों की ग़ुलामी में जकड़ा हुआ था। उनकी मातृभूमि, यहूदिया, 6 ई. में सीधे रोमन राज्यपालों के प्रशासन के अधीन आ गई जिन्हें प्रोक्यूरेटर कहा जाता था। पैग़म्बर के रूप में जब उन्होंने जनता को सत्य धर्म की ओर बुलाना शुरू किया, तो यरूशलेम का प्रोक्यूरेटर पोंटियस पीलातुस जैसा एक अन्यायी, भ्रष्ट और बेईमान व्यक्ति था। उन अधर्मी स्वामियों की ग़ुलामी में इस्राइलियों की मानसिक और नैतिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वे सत्य वचन सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मसीह की आँखों के सामने, गैलिली के शासक हेरोडियस ने हज़रत यहया (जॉन दि बैपटिस्ट) को केवल एक नर्तकी को खुश करने के लिए मार डाला था। स्वयं मसीह का मूल्य भी उनके लोगों की दृष्टि में क्या था, यह इससे स्पष्ट है कि इस्राइलियों ने बराब्बास नाम के एक डाकू के जीवन को मसीह के जीवन से अधिक मूल्यवान माना। ऐसी स्थिति में, मसीह के लिए अपने आह्वान की शुरुआत में ही युद्ध के झंडे के साथ खड़े होना और एक स्वतंत्र धार्मिक सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष करना भला कैसे संभव था? वे देख रहे थे कि यहूदियों की आत्मा निकल चुकी है, उनके चरित्र में कोई शक्ति नहीं रह गई है और उनकी राष्ट्रीयता में कोई जीवन नहीं बचा है। इसलिए, उनका पहला कार्य अपने राष्ट्र को नैतिक पतन के गड्ढे से बाहर लाना था जिसमें वह गिर गया था और उसमें नैतिक उत्कृष्टता की भावना पैदा करना था जिसके बिना कोई भी राष्ट्र ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ नहीं सकता और न दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, और न वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सकता है। अतः सर्वप्रथम उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए बराबर प्रयास करते रहे ताकि इस रचनात्मक कार्य के दौरान सरकार से टकराव की कोई सम्भावना न रहे। अगर शुरुआत से ही, सरकार के साथ टकराव हो गया होता, तो वास्तविक सुधार का काम नहीं हो पाता और सुधार न होने पर, सरकार के साथ टकराव में भी असफलता ही हाथ लगती। इसलिए उन्होंने सरकार के साथ टकराव से परहेज़ किया। जब यहूदी विद्वानों के शिष्यों ने उन्हें पकड़वाने के लिए उनसे यह सवाल पूछा कि हमें सीज़र को कर देना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने यह दुअर्थी उत्तर देकर टाल दिया:
“क्या हमें कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं।
उस ने उन की चतुराई को ताड़कर उन से कहा; एक दीनार मुझे दिखाओ। इस पर किस की मूर्ति और नाम है?
उन्होंने कहा, कैसर का।
उस ने उन से कहा; तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो।” (लूका, 20:22-25)
उन्होंने आदेश दिया कि दुष्ट से मत लड़ो, जो तुम पर अत्याचार करे उसे आशिर्वाद दो और उसके लिए समृद्धि मांगो, जो तुम्हें बेगार में पकड़े, उसके साथ एक कोस के बजाय दो कोस जाओ। जो तुम्हारा कुर्ता छीने, उसे अपना चोगा भी उतार दो; और जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उस की ओर दूसरा गाल भी फेर दो। आरंभ में, इन सभी आदेशों का उद्देश्य यह था कि सरकार के साथ कोई संघर्ष न हो और लोगों में कठिनाई झेलने की शक्ति पैदा हो जाए। उसके बाद, उन्होंने धीरे-धीरे अपने लोगों को दृढ़ता, धैर्य और निर्भयता सिखाना शुरू किया, उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार किया, और उनके दिलों से मौत के डर और संप्रभु सत्ता के प्रकोप को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा :
“परन्तु तुम अपने विषय में चौकस रहो; क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे; और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उन के लिये गवाही हो। पर अवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, तो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम क्या कहेंगे; पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना; क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई, और पिता को पुत्र घात के लिये सौंपेंगे, और लड़के-बाले माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे; पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा॥” (मरकुस,13:9-13)
उम्होंने दिलों से जान की मुहब्बत कम करने और मरने के लिए तैयार रहने के लिए उनसे कहा कि:
“क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा।” (लूका 9:24)
सरकार और उसकी व्यवस्था पर भरोसा करने के बजाय, उन्होंने अल्लाह और उसकी व्यवस्था पर भरोसा रखने की शिक्षा दी। ताकि वह सबसे बड़ी कमज़ोरी दूर हो जाए जो एक ग़ुलाम राष्ट्र को शासक राष्ट्र के अधीन रखता है। उन्होंने कहा :
“सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के-बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा॥” (लूका 11:13)
उन्होंने प्रशासन के भय को दूर करने का प्रयास किया और उनसे कहा कि जो केवल शरीर को मार सकते हैं वे आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरना तो सचमुच उस से चाहिए जो प्राण और शरीर दोनों पर मृत्यु ला सकता है।
“परन्तु मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूं, कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते उन से मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने के बाद जिस को नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो : वरन मैं तुम से कहता हूं उसी से डरो।” (लूका 12:4-5)।
सदियों से ग़ुलामी में बंधे लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता पैदा करने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक थीं, और शुरू में मसीह ने अपनी शिक्षा को इन्हीं चीज़ों तक सीमित कर दिया। इस पड़ाव को पार करने के बाद अन्तिम काल में वे संघर्ष और लड़ाई के विषयों की ओर बढ़ने लगे। कभी-कभी वे अपने शत्रुओं को मारने की इच्छा भी दिखाने लगे। एक अवसर पर वे कहते हैं:
“परन्तु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उन को यहां लाकर मेरे सामने घात करो॥” (लूका 19:27)
इसी तरह, उन्होंने अपने अनुयायियों को तलवारें रखने का भी आदेश दिया, जैसा कि लूका ने लिखा है:
“उस ने उन से कहा, परन्तु अब जिस के पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिस के पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि यह जो लिखा है, कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा; हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारें हैं: उस ने उन से कहा; बहुत हैं॥” (लुका, 22:36-38)
लेकिन मसीह को अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए केवल ढाई से तीन साल की अवधि मिली। यह छोटी अवधि एक पूरे राष्ट्र को अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस दौर में न तो उसके अनुयाइयों की संख्या इस हद तक पहुँची थी कि वे रोमनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकें और न ही उसके अनुयायी बनने वालों का नैतिक प्रशिक्षण इतना पूर्ण था कि वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सभी प्रकार के ख़तरों का सामना करने को तैयार होते। उन लोगों का विश्वास अभी इतना मज़बूत नहीं था कि वे खुले तौर पर सच्चाई को व्यक्त करने का साहस कर पाते। मसीह के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र पतरस की यह स्थिति थी कि उसकी गिरफ़्तारी के समय जब उससे पूछा गया कि क्या तुम भी मसीह के अनुयायी हो, तो उसने मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तीन बार मसीह का इनकार कर दिया।
“जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई। और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है: फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया; और मुर्गे ने बांग दी। वह लौंडी उसे देखकर उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, कि वह उन में से एक है। परन्तु वह फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; निश्चय तू उन में से एक है; क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने देने और शपथ खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहीं जानता। तब तुरन्त दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी: पतरस को वह बात जो यीशु ने उस से कही थी स्मरण आई, कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को सोचकर रोने लगा॥” (मरकुस, 14: 66-72)
उनके एक अन्य शिष्य, यहूदा इस्करियोती ने चाँदी के मात्र 30 सिक्कों के लिए उन्हें गिरफ़्तार करा दिया:
“तब यहूदा इस्करियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे तीस चान्दी के सिक्के तौलकर दे दिए। और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढ़ने लगा॥” (मत्ती, 26:14-16)
फिर जब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, तो उनके सभी शिष्य उन्हें छोड़कर भाग गए:
“परन्तु यह सब इसलिये हुआ है, कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन के पूरे हों: तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए॥ और यीशु के पकड़ने वाले उस को काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरिनए इकट्ठे हुए थे।” (मत्ती, 26:56-57)
ज़ाहिर है कि जब उनके ख़ास अनुयायी और विश्वस्त शिष्यों की स्थिति ऐसी थी, तो वे इतनी अविश्वसनीय सेना को साथ लेकर जिहाद छेड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? अगर उन्हें भी अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की तरह शिक्षा और प्रशिक्षण का पर्याप्त अवसर मिलता, तो यह संभव था कि वे भी अपने अनुयायियों में बहादुरी की वही भावना पैदा कर देते। लेकिन उनकी बिगड़ैल क़ौम ने उनकी नुबूवत को पूरे तीन साल तक भी बरदाश्त न किया और उन्हें इतना वक़्त भी नहीं दिया कि वे उनकी भलाई के लिए कोई बड़ा काम कर सकते। इस छोटे से समय में जितना काम किया जा सकता था उतना काम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने किया। अगर हम मुहम्मद (सल्ल.) के मक्का जीवन के पहले तीन वर्षों को देखें, तो उसमें कहीं भी जिहाद और लड़ाई का कोई निशान नहीं होगा। धैर्य और सहनशीलता, दृढ़ता, पवित्रता और भय, अल्लाह पर भरोसा और आत्म-शुद्धि और नैतिकता की वही शिक्षाएँ वहाँ पाई जाएँगी जो मसीह के पैग़म्बराना जीवन में पाई जाती हैं।
ईसाइयत और यहूदी धर्मविधान का संबंध
अगर इस ज्ञान और अंतर्दृष्टि के प्रकाश में मसीह की शिक्षाओं का विश्लेषण किया जाए, तो उन्हें दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाएगा:
एक प्रकार वह है जिसमें मसीह ने हज़रत मूसा द्वारा बनाए क़ानूनों को पूरा किया और उसमें आवश्यक परिवर्धन किया। उनके क़ानूनों में कोई लचीलापन नहीं था और उनकी शिक्षाओं में मानव समुदाय की व्यापक कल्पना बहुत धुंधली थी, मसीह ने इस कमी को पूरा किया और इस्राइलियों को सभी मानव जाति से समान रूप से प्रेम करने का उपदेश दिया। उसमें मनुष्य के मात्र दायित्वों पर ज़ोर दिया गया था और परोपकार या नैतिक गुण के हिस्से को अछूता छोड़ दिया गया था। मसीह ने इस पहलू पर सबसे अधिक ज़ोर दिया और दान, उदारता, करुणा, आत्म-त्याग और दया का उपदेश दिया। मसीह की शिक्षा का यह हिस्सा अपने आप में एक स्थायी क़ानून नहीं था, बल्कि हज़रत मूसा द्वारा बनाए क़ानूनों के लिए एक आवश्यक पूरक था।
दूसरा प्रकार वह है जिसमें हज़रत ईसा ने अपने समय के इस्राईलियों की विशिष्ट नैतिक, सामूहिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुधार करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, यहूदियों में धन का लालच और दुनिया का प्यार बहुत बढ़ गया था। हज़रत ईसा ने संतोष और दुनिया की दौलत की तुच्छता पर ज़ोर दिया। यहूदियों में कठोरता की अधिकता थी, जवाब में, मसीह ने क्षमा और दया का उपदेश दिया। यहूदियों में कंजूसी और संकीर्णता व्याप्त थी, मसीह ने उनके सुधार के लिए उदारता की शिक्षा दी। यहूदी सरदार और धर्मगुरु आत्म-केन्द्रित और अभिमानी थे। हज़रत ईसा, ने उन्हें संयम में लाने के लिए विनम्रता, त्याग, तपस्या, धर्मपरायणता और अल्लाह के भय पर ज़ोर दिया। यहूदी राष्ट्र रोमन सरकार के अधीन ग़ुलाम, असहाय और कमज़ोर था। उनकी सुरक्षा और मुक्ति के लिए ईसा मसीह ने एक ओर तो उन्हें सरकार से टकराने से रोका, उन्हें अत्याचार सहने का उपदेश दिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करने से मना किया और दूसरी ओर उनमें आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करने के लिए धैर्य, दृढ़ता, निर्भयता, परिपक्वता और दृढ़ संकल्प की शक्ति बनाने की कोशिश की।
मसीह के शिक्षण का यह दूसरा भाग, इस्राईलियों की उस स्थिति के लिए विशिष्ट था जिसमें वे मसीह के आगमन के समय लिप्त थे। इसे स्थायी और सार्वभौमिक क़ानून बनाने का इरादा कभी नहीं था। यह शिक्षा कि तुम दुष्ट का सामना न करो, जो एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, और जो तुम्हारा कुर्ता छीने, उसे अपना चोगा भी उतार कर दे दो, यह वास्तव में दासता की एक विशिष्ट दशा के लिए थी। इसे स्वतंत्र राष्ट्र की राजनीतिक नीति बनाना न तो वांछनीय था और न ही किसी प्रकार से यह सही और युक्तियुक्त हो सकता था।
धर्मविधान और ईसाइयत का पृथक्करण:
लेकिन ईसा मसीह के इस दुनिया से जाने के कुछ ही साल बाद, वे सभी सिद्धांत और नियम, जिन पर उन्होंने अपने धार्मिक नवीनीकरण और सुधार को आधारित किया था, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और ईसा की मूल शिक्षा को इस तरह बदल दिया गया कि दुनिया में उसके अस्तित्व का कोई निशान तक बाक़ी नहीं रहा। विकृति की इस प्रक्रिया का प्रेरक सेंट पॉल था। हम उसकी मंशा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यह संभव है कि ईसा मसीह के जीवन काल में और उनके बाद भी 6 वर्षों तक ईसा के आहवाण का घोर विरोधी रहने के बाद अंतत: वह सच्चे हृदय से ईसा का अनुयायी और हिमायती बन गया हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह न तो मसीह के साथियों में से था, और न उसे मसीह के प्रशिक्षण में रह कर मसीह की शिक्षाओं की सच्ची भावना को समझने का कोई अवसर मिला था।
ख़ुद सेंट पॉल के शिष्य ल्यूक की किताब “एक्ट्स” से साबित होता है कि ईसा मसीह के जीवन के दौरान, उसको उनकी संगति और प्रशिक्षण से लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं मिला था। साथ ही जब उसने ईसा के धर्म को विकृत करना शुरू किया तो ईसा के विशेष रूप से प्रशिक्षित शिष्यों ने उसका कड़ा विरोध किया। अतः स्वयं गॉस्पेल के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संत पॉल द्वारा आविष्कृत सिद्धांत न केवल ईसा के धर्म की भावना के विरुद्ध थे, बल्कि स्वयं ईसा के स्पष्ट निर्देशों के भी विरुद्ध थे।
इस संबंध में, पॉल ने धर्म के सिद्धांत में जो पहली विकृति की, वह यह थी कि उसने मसीह की शिक्षा को सभी मानव जाति के लिए एक सामान्य संदेश के रूप में घोषित किया। हालांकि असल में ये केवल बनी इसराईल के लिए थी। मसीह ने अपने जीवन में जब अपने शिष्यों को उनके प्रचार करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि:
“इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्यजातियों की ओर न जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। परन्तु इसराईल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना।” (मत्ती, 10:5-6)
स्वयं हज़रत ईसा ने कभी भी एक पल के लिए भी ग़ैर-इस्राईली क़ौमों को अपनी ओर आमंत्रित नहीं किया और किसी भी ग़ैर-इस्राईली को अपनी मण्डली में प्रवेश नहीं दिया। संत पॉल के प्रकट होने से पहले, मसीह के शिष्य भी इस्राइलियों को ही आमंत्रित करते रहे। उपदेशक भी इस्राईली था और संबोधक भी इस्राईली थे। उस समय तक, मसीह का आहवाण यहूदी धर्म में सुधारवादी आंदोलन माना जाता था। (मिलमैन हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, वॉल्यूम I, पृ. 377)
शिष्यों के बीच यह पूरी तरह विदित था कि बाइबल का प्रचार केवल उनके लिए है जो मूसा की शरीयत का पालन करते हैं। (डुमेलो, कमेंट्री ऑन दि होली बाइबल, P.LXXXIX)
मसीह के अनुयायियों का एक बड़ा जनसम्मेलन जो 49 ईस्वी में यरूशलेम में आयोजित हुआ था, उस में एक बड़ा वर्ग इस मत का समर्थक था। (मिलमैन हिस्ट्री ऑफ क्रिस्चियनिटी, वॉल्यूम I, पृष्ठ 393)
लेकिन पॉल ने मसीह के आहवाण की वास्तविकता विकृत की, मसीह की विशिष्टताओं, और शिष्यों के ज्ञान और विश्वास को नज़रअंदाज़ कर दिया और फ़ैसला किया कि मसीह का आहवाण दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए है। और इस फैसले को सही ठहराने के लिए, उसने दावा किया कि मसीह ने सूली पर चढ़ने और मरने के बाद, आकर अपने शिष्यों को आदेश दिया था, “जाओ और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ।” (डुमेलो, कमेंट्री ऑन दि होली बाइबल, P.LXXXIX)
“इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रआत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।” (मत्ती, 28:19)
लेकिन ग़ैर-इसराईली राष्ट्रों से मूसा के नियमों का पालन करवाना कठिन था। बहुत से धार्मिक अनुष्ठान ऐसे थे जिनसे उन राष्ट्रों को घृणा थी। इसलिए, तुरंत यह सवाल उठा कि जब उन राष्ट्रों को ईसाई धर्म में आमंत्रित किया जाए, तो क्या हज़रत मूसा के क़ानूनों के पालन पर ज़ोर दिया जाए या नहीं? इस संबंध में, मसीह के विनिर्देश बहुत स्पष्ट थे, उन्होंने कहा था कि ज़मीन और आकाश टल सकते हैं, मगर तोराह का एक बिंदु भी नहीं टल सकता है। और यह कि “मैं तोराह को निरस्त करने नहीं, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ” और “जो तोराह के आदेशों का पालन करे, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है।” इन निर्देशों के बाद, किसी सच्चे ईसाई के लिए ईसाई धर्म को हज़रत मूसा के क़ानूनों से अलग करना संभव नहीं था। लेकिन पॉल ने उनके विपरीत फ़ैसला किया कि हर ग़ैर-इस्राईली ईसाई बन सकता है, चाहे वह हज़रत मूसा के क़ानूनों का पालन करे या न करे। (मिलमैन हिस्ट्री ऑफ क्रिस्चियनिटी, वॉल्यूम I, पृष्ठ 392)
इस प्रकार, वे सभी ग़ैर-इस्राईली बहुदेववादी जो हज़रत मूसा के क़ानूनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकार करते थे, ईसाई धर्म में शामिल कर लिए गए।
इस संशोधन और विकृति का विरोध किया गया (अधिनियम, अध्याय 21) और यहाँ तक कि ईसाई समुदाय के बुजुर्गों ने भी इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन पॉल ने सेंट पीटर और सेंट बरनबास जैसे महान प्रेरितों को पाखंडी और विधर्मी ठहरा दिया (गलतियों 2:13) और खुले आम हज़रत मूसा के क़ानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया। वह गलातियों को लिखे अपने पत्र में लिखता है:
“तौभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें; इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैं ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है: और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस ने मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धामिर्कता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता॥” गलतियों (2:16-21)
“सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के आधीन हैं, क्योंकि लिखा है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; पर जो उन को मानेगा, वह उन के कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिये श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है।” (3:10-13)
“इसलिये व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परन्तु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के आधीन न रहे।” (3:24-25)।
“मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें स्वतंत्र किया है; सो इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जूए में फिर से न जुतो॥ देखो, मैं पौलुस तुम से कहता हूं, कि यदि खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं, कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि आत्मा के कारण, हम विश्वास से, आशा की हुई धामिर्कता की बाट जोहते हैं।” (5:1-5)
इस प्रकार ईसाई धर्म हज़रत मूसा के धर्मविधान से अलग हो गया। सभ्यता-संस्कृति, समाज, राजनीति तथा सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सभी क़ानूनों को रद्द कर दिया गया। और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक अधूरा संग्रह, जो धर्मविधान के पूरक के रूप में एक विशेष राष्ट्र की विशेष स्थिति को ठीक करने के लिए तैयार किया गया था, एक स्थायी, सार्वभौमिक और सर्वकालिक धर्म बना दिया गया।
ईसाई चरित्र पर पृथक्करण का प्रभाव
सेंट पॉल के अनुकरणकर्ताओं ने इस अपूर्ण धर्म को, जो वास्तव में ईसाई नहीं बल्कि पॉलीन धर्म था, इस्राईलियों को छोड़कर, रोम और ग्रीस के स्वतंत्र समुदायों में फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी धर्मविधान और क़ानून के बिना ही मात्र एक नैतिक शिक्षा के रूप में और वह भी एक ऐसी नैतिक शिक्षा जो वास्तव में एक ग़ुलाम और पिछड़े राष्ट्र के लिए डिज़ाइन की गई थी और जो स्वतंत्र और स्व-शासित राष्ट्रों के लिए बिल्कुल बेकार और अर्थहीन थी। उसमें ऐसा कोई पूर्ण निर्देश नहीं था जो विभिन्न परिस्थितियों में सामान्य मानव समुदाय के लिए उपयोगी और उपयुक्त हो सके। वह केवल नैतिक सलाहों का एक ऐसा संग्रह था, कि किसी राष्ट्र के लिए केवल उनका अनुसरण करके जीवित रहना असंभव था। इसलिए परिणाम यह हुआ कि पहले ढाई से तीन सौ वर्षों तक तो ईसाई हर प्रकार की क्रूरता और हिंसा का शिकार बनते रहे, क्योंकि उन्हें यही नैतिकता सिखाई गई थी और इस लक्ष्य से आगे चलने के लिए उनके पास कोई दिशा-निर्देश नहीं था। फिर जब संयोगवश उन्हें सत्ता मिल गई, तो उनके लिए पॉलीन ईसाई धर्म के अव्यवहारिक सीमा में रहना असंभव हो गया। इसलिए, उन्होंने ईसाई धर्म की सभी नैतिक सीमाओं को तोड़ दिया और उत्पीड़न, अत्याचार, हिंसा और हत्या की अति कर दी।
शुरुआत में, तो ईसाइयों को आश्वासन दिया गया था कि एक गाल के साथ दूसरा गाल भी बढ़ा देना और दुष्टों का कभी विरोध नहीं करना मसीह की सर्वकालिक शिक्षा है। इसलिए, जब उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हो गई और उनका प्रभाव फैल गया, तब भी वे उत्पीड़न से लड़ने और अपने अधिकारों की रक्षा करने की भावना विकसित नहीं कर सके। 64 ईस्वी में जब ग्रीस और रोम और सीरिया और फ़िलिस्तीन में ईसाइयों की संख्या हज़ारों से अधिक हो गई थी, तो नीरो ने उन पर रोम को जलाने का झूठा आरोप लगाया और अपने आदेश से उन सभी को गिरफ़्तार कर लिया। कुछ को सूली पर चढ़ाया गया, कुछ को ज़िंदा जला दिया गया, कुछ को कुत्तों से टुकड़े-टुकड़े करा दिया गया। सैकड़ों ईसाई महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को रोम के अखाड़ों में क्रूर खेलों में इस्तेमाल किया जाने लगा। 70 ई. में, टाइटस के नेतृत्व में, यरूशलेम पर हमला किया गया। 97 हज़ार लोगों को गिरफ़्तार कर के दास बना लिया गया, 11 हज़ार लोगों को भूखा मार दिया गया, हज़ारों लोगों को रोम के अखाड़ों और इम्फी थियेटरों में जंगली जानवरों का निवाला बनने या सयाफों की तलवारबाज़ी के अभ्यास में काम आने के लिए भेज दिया गया। (गिबन वॉल्यूम- II, चैप-16, अर्ली डेज़ ऑफ क्रिसचनिटी, पीपी.488-89)
नीरो के बाद, मार्कस ऑरेलियस, सेप्टिमस, सेवरस, डेसियस और वेलेरियन ने ईसाई धर्म और उसके अनुयायियों को कुचलने का प्रयास किया। अंत में, डेव क्लिशियन ने तो अत्याचार और उत्पीड़न की अति कर दी। उसने गिरजाघरों को गिराने, बाइबल जलाने और गिरजाघरों की सम्पत्ति ज़ब्त करने के सामान्य आदेश जारी कर दिए। 303 ई. में, सम्राट ने स्वयं निकोमेदिया के मुख्य चर्च को ध्वस्त कर दिया और पवित्र किताबों को जलवा दिया। 304 ई. में उसने सामान्य आदेश दिया कि जो कोई भी ईसाई धर्म छोड़ने को तैयार न हो, उसे मार दिया जाए। उसके बाद, सख़्ती और उत्पीड़न बढ़ गया। यहां तक कि ईसाई धर्म को छोड़ने से इनकार करने वालों के शरीर को घायल कर के उसपर, सिरका और नमक डाल दिया जाता, और बाद में उसकी बोटी-बोटी काटी जाती। कभी-कभी उन्हें चर्च में बंद कर के आग लगा दी जाती। अधिक आनंद लेने के लिए, एक-एक ईसाई को पकड़कर दहकते अंगारों पर लिटा दिया जाता था या उसके शरीर में लोहे की कीलें ठोंक दी जाती थीं। यह वह समय था जब कि ईसाई पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। साम्राज्य के छोटे-बड़े पद बड़ी संख्या में उन के हाथ में थे। और स्वयं सम्राट के महल में ईसाइयों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी। (रेव. कट्स, कांस्टेनटाइन द ग्रेट पीपी.55-60)
लेकिन ईसाइयों को विश्वास दिलाया गया था कि चाहे तुम बहुतायत में हो और चाहे तुम्हें शक्ति भी प्राप्त हो, फिर भी, बुराई का विरोध न करने और एक गाल के साथ दूसरा गाल बढ़ाने की शिक्षा ही व्यवहार्य है। जो शिक्षा इस्राइलियों को अत्यधिक लाचारी और कमज़ोरी की स्थिति में दी गई थी। इसलिए सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक़, मिस्र, अफ्रीका, स्पेन, गॉल, सिलेसिया, इटली, इलेरिया, एशिया माइनर में कहीं भी ईसाइयों ने इन अत्याचारों का विरोध नहीं किया और पूरा समुदाय इन कार्रवाइयों को कायरता के साथ सहन करता रहा। इसके विपरीत अरबी रसूल की उम्मत जिसे जिहाद की शिक्षा दी गई थी, जब 250-300 की संख्या तक पहुँच गई, तो वह पूरे अरब जगत का सामना करने के लिए खड़ी हो गई और उसने दुनिया को बता दिया कि जिस समुदाय में यह मुजाहिदाना भावना मौजूद हो, वह संख्या की कमी और अभावग्रस्तता के बावजूद किसी से दब कर नहीं रह सकती।
यह तो थी ईसाइयत की एक अति। उसके बाद, जब कॉन्सटेंटाइन द ग्रेट ने इसे स्वीकार कर लिया और यह साम्राज्य का वास्तविक धर्म बन गया, तो यह यहां से छलांग लगाकर अचानक दूसरी अति पर पहुंच गया। पहला दोष इस तथ्य के कारण था कि पॉलीन ईसाई धर्म का राजनीति और सभ्यता से कोई लेना-देना नहीं था और उसके अनुयायी अपने धर्म का पालन करते हुए एक विशुद्ध निष्क्रिय जीवन अपनाते थे। लेकिन जब संयोग से साम्राज्य की जिम्मेदारियां उन पर आ पड़ीं तो दूसरी, और पहली से अधिक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। चूंकि ईसाइयत ने उन्हें शासन के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने इस पूरे कारोबार को अल्लाह की नियमावलि के बजाय अपने मन की इच्छा के अनुसार चलाना शुरू कर दिया। साम्राज्य के मामलों में, तो युद्ध भी है और शांति भी, राजनीति भी है और दंडविधान भी, बदला भी है और क्षमा भी। लेकिन हज़रत मूसा के लाए क़ानूनों से अलग किए ईसाई धर्म में इनमें से किसी भी कार्य के लिए कोई नियम और क़ानून नहीं था। उसने इस एक नियम के सिवा कि दुष्टों का विरोध न करो और कुर्ता छीनने वाले को चोग़ा भी उतार कर दे दो, जीवन के कामों के लिये और कोई नियम न बनाया था। मगर निष्क्रियता और अपमान के शिक्षण की इस संकीर्ण सीमा में रहकर ईसाइयों के लिए साम्राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को अंजाम देना असंभव था। इसलिए उन्हें इस घेरे को तोड़कर बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब उन्होंने इसे तोड़ दिया, तो वे अपनी मनेच्छा के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इस व्यवहारिक दुनिया में उनके लिए ऐसा कोई धार्मिक मार्गदर्शन और दिव्य प्रकाश नहीं था जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकता। परिणाम यह हुआ कि ईसाइयों ने अल्लाह की भूमि में उत्पात मचाना और अव्यवस्था फैलाना शुरु कर दिया और उद्दंडता और बिगाड़ का ऐसा कोलाहल मचाया जो आज तक ठंडा नहीं हो सका।
कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान, साम्राज्य के लगभग आधे निवासी मूर्तिपूजक थे, इसलिए उसने उन्हें अधिक प्रताड़ित करने का साहस नहीं किया। इतना ही किया कि मंदिरों के दरवाज़े और उनकी छतें ध्वस्त कर दीं, मूर्तियों के कपड़े और गहने उतरवा लिए और उन्हें मंदिरों से बाहर निकलवा दिया।(रेव. कट्स, कॉन्सटेंटाइन द ग्रेट)। पृ. 278)
फिर कुछ वर्षों बाद, जब चर्च ने देश पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो ईसाई धर्म के नेताओं ने विधर्मियों को कुचलने का फ़ैसला किया और धार्मिक क़ानूनों के अनुसार निम्नलिखित दो सिद्धांत स्थापित किए, जिनसे दूसरे धर्मों को कुचलने के कई आदेश निकलते थे:
1) जिन पापों पर दंडाधिकारी न तो रोक लगाता है और न ही दंड देता है, वह स्वयं कुछ हद तक उन पापों के उत्तरदायित्व में भागीदार होता है।
2) कृत्रिम देवताओं और वास्तविक दुष्ट आत्माओं की मूर्तिपूजा करना सृष्टिकर्ता के विरुद्ध एक घिनौना अपराध है।
इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए, रोमन सिनेट ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी कि “रोमनों का धर्म बृहस्पति की पूजा नहीं है, बल्कि ईसा मसीह की पूजा है। उसके बाद, मूर्तियों की पूजा और उनपर चढ़ावे और बलिदान सबकुछ क़ानून द्वारा निषिद्ध ठहरा दिया गया, और इन कृत्यों के अपराधियों के लिए कड़ी सज़ा निर्धारित की गईं। राजा थियोडोसियस ने अपने आदेशों में ग़ैर-ईसाई पूजा के सभी रूपों को मना कर दिया, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी। उन्होंने उसे राज्य के ख़िलाफ़ विद्रोह ठहराते हुए घोषणा की और उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान रखा। इसके साथ ही उसने मंदिरों को गिराने, उनकी संपत्तियों को ज़ब्त करने और पूजा की चीज़ों को नष्ट करने का एक सामान्य आदेश भी जारी किया। इस आदेश के अनुसार, सबसे पहले, केंद्र सरकार में बुतपरस्ती को समाप्त कर दिया गया। फिर प्रांतों में भी उसे दोहराया गया। गॉल प्रांत में, वृषभ के बिशप ने धर्मपरायण पुजारियों की एक सेना लेकर मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। यहां तक कि उन वृक्षों को भी नष्ट कर दिया, जिन्हें पवित्र माना जाता था।
सीरिया में ईसाई धर्म के पवित्र धर्मगुरु डायोसेस ऑफ अपामिया के धर्माध्यक्ष मार्सेलस ने जुपीटर के भव्य मंदिर को ढहा दिया और अपने क्षेत्र के ग़ैर-ईसाइयों के पूजास्थलों को तोड़ने के लिए एक पूरी सेना भेज दी। अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र के आर्चबिशप थियोफिलस ने सेरएपिस के मंदिर को, जो ग्रीक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, नष्ट कर दिया। उनकी लाइब्रेरी, जिसमें बटालसा परिवार ने विज्ञान और कला का सबसे अच्छा संग्रह एकत्र किया था, को आग लगा दी। सेरएपिस की मूर्ति को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, उसकी भुजाओं को अलेक्जेंड्रिया के बाज़ारों में घसीटा गया, ताकि उसके भक्तों को पीड़ा पहुंचे और अंत में हज़ारों लोगों के सामने उसके टुकड़ों को जला दिया गया। इसी तरह, अन्य प्रांतों में भी, “धार्मिक कट्टरपंथियों की एक पूरी सेना बिना किसी अधिकार और अनुशासन के शांतिपूर्ण निवासियों पर हमले करती थी और प्राचीन वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूनों को नष्ट करती फिरती थी।
ये सभी विवरण गिब्बन की पुस्तक ‘रोमन साम्राज्य के पतन का इतिहास’ के अध्याय 28 से लिए गए हैं।
इन क्रूरताओं का परिणाम यह हुआ कि मूर्तिपूजक प्रजा ने तलवार के भय से उस धर्म को स्वीकार कर लिया जो उन्हें हृदय से पसन्द नहीं था, और ईसाई गिर्जाघर हृदयहीन और अविश्वासी अनुयायियों से भर गया। 38 वर्षों के भीतर, रोम के महान साम्राज्य से मूर्तिपूजा का सफ़ाया हो गया और यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में तलवार के बल पर ईसाई धर्म फैल गया।
उस के बाद से ईसाइयों और ग़ैर-ईसाइयों के बीच और स्वयं ईसाइयों में परस्पर जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें नैतिकता और मानवता के सिद्धांतों की अवहेलना करके, युद्ध के ऐसे बर्बर तरीक़े अपनाए गए हैं, जिनके भयानक उल्लेख से इतिहास के पन्ने काले हैं। ग़ैर-ईसाई मान्यताओं को मिटाने के लिए बल-प्रयोग के जिन तरीक़ों को ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा उचित ठहराया गया था, उनका एक नमूना वे धार्मिक अदालतें हैं जो धर्माधिकरण के नाम से, ख़ुद रोमन पोप के तहत स्थापित की गई थीं। उनमें नास्तिकता, यहूदी धर्म, इस्लाम और बहुविवाह जैसे “अपराधों” की सज़ा देने के लिए जो दंडविधान प्रचलित था, उसमें बहुत से दंडों के साथ, व्यक्ति को ज़िंदा जलाना, जीभ काट देना और मृत व्यक्ति की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को बाहर फेंकना भी शामिल था। अकेले स्पेन में ही इस धार्मिक न्यायालय के आदेश से तीन लाख चालीस हज़ार लोग विभिन्न प्रकार से मार डाले गए, जिनमें 32 हज़ार वे हैं, जिन्हें ज़िंदा जला दिया गया। इसके अलावा, मेक्सिको, कार्टाजेना, सिसली, सार्डिनिया, माल्टा, नेपल्स, मिलान, फ़्लैंडर्स, आदि के धार्मिक न्यायालयों ने ग़ैर-ईसाई आस्था रखने के कारण जितने लोगों को मार डाला, उनकी संख्या का न्यूनतम अनुमान डेढ़ लाख किया गया है।(एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आर्ट, “इनक्विजिशन”)
यह पॉलिन ईसाई धर्म की त्रुटिपूर्ण शिक्षा का दूसरा परिणाम है। पहला परिणाम तो यह हुआ था कि जब ईसाईयों ने इस धर्म के उपदेशों का पालन किया, तो वे बहुत नर्म बन गए, और प्रतिरोध की अपनी क्षमता के बावजूद, वे तीन सौ वर्षों तक उत्पीड़न सहते हुए ख़ुद को नष्ट कराते रहे। और दूसरा परिणाम यह हुआ कि जब समय के परिवर्तन ने उन्हें शक्ति प्रदान की और साम्राज्य की ज़िम्मेदारी उन पर आ पड़ी तो उन्हें ईसाइयत के संकीर्ण दायरे को छोड़ना पड़ा और यहां धर्म का कोई निर्देश और मार्गदर्शन न पाकर उन्होंने अपने ही लोगों पर हर तरह का अत्याचार करना शुरू कर दिया और मनेच्छा के पालन में स्वच्छंदता के साथ जो करना चाहा वह किया।
तीसरा और अंतिम परिणाम यह हुआ कि जब धर्म के नाम पर दमन, अत्याचार और अज्ञानतापूर्ण धर्मांधता की आँधी ने हद पार कर दी तो उन्हें धर्म से ही नफरत हो गई और वे संसार भर में अधर्म फैलाने के लिए उठ खड़े हुए।
इसमें कोई संदेह नहीं कि अत्याचार कुछ मुस्लिम राजाओं ने भी किये। युद्ध के बर्बर तरीक़े कुछ लड़ाइयों में मुसलमानों ने भी अपनाए हैं। धर्म के नाम पर अधार्मिक युद्ध लड़ने के दाग़ से मुसलमान भी बचे हुए नहीं हैं। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि मुसलमानों के किसी भी कार्य की ज़िम्मेदारी इस्लाम पर नहीं आती है, क्योंकि इसने उनकी सभी प्राकृतिक ज़रूरतों के लिए पूरे क़ानून बना कर दिए हैं, जिनमें न तो अप्राकृतिक सीमाएं या बंदिशें हैं, जिनका पालन असंभव हो और न ऐसी खुली स्वतंत्रता कि मनुष्य जो चाहे करे। इसलिए इस्लाम के अनुयायियों के जो अनुचित व्यवहार हैं, वे वास्तव में क़ानून तोड़ने की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी क़ानून पर नहीं पड़ती। इसके विपरीत ईसाई धर्म ने अपने अनुयायियों के व्यवहारिक जीवन के लिए कोई नियम बना कर नहीं दिया। उसने यह नहीं बताया कि अगर आप कमज़ोर हैं तो शक्ति कैसे प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त होने पर उसका उपयोग कैसे करें। अन्य राष्ट्रों के साथ शांति हो तो किस सिद्धांत पर हो, युद्ध हो तो किन उद्देश्यों के लिए हो। युद्ध के मैदान में शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, जीत मिल जाए तो शत्रुओं के साथ क्या व्यवहार करें। दूसरे धर्म के लोगों के साथ मामला करें तो कैसे करें, किन मामलों में उनके साथ सख़्ती करें। इसलिए ईसाई धर्म के अनुयायियों ने पहले उसके घेरे में रहकर और फिर उसके घेरे को तोड़कर जितने नैतिक अपराध किए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी में ख़ुद ईसाई धर्म भी शामिल है। क्योंकि इसने उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखाया। इस्लाम की तरह, ईसाई धर्म अपने अनुयायियों के अपराधों से ख़ुद को यह कह कर बरी नहीं कर सकता, कि उन्होंने इसके द्वारा दिए गए सिद्धांतों और नियमों का पालन नहीं किया। वह इन दो मामलों में से एक को अपनाने के लिए मजबूर है, या तो उन सभी ईसाइयों को अपराधी ठहराए, जिन्होंने राजनीति और सरकार की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है, चाहे उन्होंने इसे सही तरीक़े से पूरा किया हो या ग़लत तरीक़े से। या उन सभी ईसाइयों को बेगुनाह ठहराना होगा, जिन्होंने सत्ता का बोझ उठाया और उसे पूरा किया चाहे सही तरीक़े से या ग़लत तरीक़े से। वह इन दोनों के बीच कोई तीसरा मामला नहीं बना सकती, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों ही मामले तर्कहीन हैं।
(5) चारों धर्मों की शिक्षाओं पर एक नज़र
हमने यहाँ युद्ध के विषय में विश्व के चार प्रमुख धर्मों के मतों की व्याख्या कर दी है। ये मत दो अतियों के अलग-अलग नमूने पेश करते हैं। पहले उल्लिखित दो मत युद्ध को उचित ठहराते हैं, लेकिन इस तरह कि वे मनुष्य को उन सभी लक्ष्यों के लिए लड़ने की अनुमति देते हैं जिनकी इच्छा उसका मन करे। वे लक्ष्यों और उद्देश्यों में सही और ग़लत के बीच अंतर नहीं करते हैं, वे मनुष्य के सामने कोई उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हैं। किसी उच्च नैतिक उद्देश्य की ओर उसका ध्यान नहीं दिलाते, बल्कि शुद्ध पाश्विक प्रवृति के आधार पर, उसे यह अधिकार देते हैं कि वह जब चाहे, जिस तरह चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे, अपने जैसे इनसानों की हत्या कर सकता है और उन से जो चाहे छीन सकता है। उन्होंने सभ्यता की दिशा में कुछ प्रगति की भी तो केवल यह कि युद्ध के कुछ तरीक़े निर्धारित कर दिए हैं, और अपने अनुयायियों से मांग की है कि जब भी वे अपनी तरह के इनसानों का शिकार करना चाहें, तो उक्त तरीक़े से करें और उक्त तरीक़े से न करें। साथ ही, उन्होंने मानवता को भौगोलिक, जातीय, भाषाई और नस्लीय आधारों पर विभाजित किया है और किसी विशेष जाति के लोगों को कुछ ऐसी रियायतें दीं जो अन्य किसी भी जाति को नहीं दी गई।
दूसरी ओर, बाद के दो धर्मों को लगता है कि मनुष्य को स्वयं मनुष्य का शिकार करने की स्वतंत्रता देना सही नहीं है, लेकिन यह भावना उन्हें एक और चरम बिंदु पर ले जाती है। वे युद्ध से लड़ते-लड़ते मानव स्वभाव से ही लड़ने लगते हैं। अल्लाह ने मनुष्य के जीवन में संयम बनाए रखने के लिए मनुष्य में जो विभिन्न ताक़तें जमा की हैं, उनमें से कुछ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं और उनमें से कुछ को पूरी मानव प्रकृति पर हावी कर देने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि जो लोग उनके निर्देशों का पालन करते हैं वे पतन और अधीनता की गहराई में गिर जाते हैं। और जो लोग स्वभावतः स्वयं को उनके पालन में सक्षम नहीं पाते और अपने मानवीय दायित्वों को निभाने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें व्यावहारिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन का प्रकाश नहीं मिलता। फिर वे अपनी स्वयं की कल्पनाओं और मन के झुकावों का अनुसरण करके कभी इधर, कभी उधर भटकते फिरते हैं।
अतिवाद के इन दो चरम बिंदुओं के बीच इस्लाम ने संयम का एक मध्य मार्ग निकाला है। वह मानव स्वभाव और मानव ज़रूरतों और सबसे बढ़कर मानवता के सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युद्ध को दो प्रकारों में विभाजित करता है। एक वह युद्ध जो स्वार्थ के लिए धन और सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ा जाता है। दूसरा युद्ध वह है जो सत्य के समर्थन और अत्याचार के उन्मूलन के लिए लड़ा जाता है। पहले युद्ध को वह फ़ितना और बिगाड़ के रूप में वर्णित करता है, और इसे सबसे बड़ा अपराध ठहराता है और इससे पूरी तरह से बचने का आदेश देता है। दूसरे प्रकार का युद्ध उसके अनुसार अगर विशुद्ध रूप सत्य के लिए किया जाए और उसमें कोई स्वार्थ शामिल न हो, तो वह अल्लाह के रास्ते में जिहाद है, सबसे अच्छी इबादत है, सबसे पवित्र दायित्व है और इससे बेहतर मानवता की कोई सेवा नहीं है। फिर उसने इस इबादत की सीमा तय की है, इसके अवसर बताए हैं, इसके उद्देश्य बताए हैं और इसके तरीक़े पूरी स्पष्टता के साथ बताए हैं ताकि अल्लाह के नाम पर शैतान का काम न होने लगे और लोग अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए ग़लत रास्ते पर न पड़ जाएं।
यह एक पूरी क़ानून संहिता है जो इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म या संस्कृति में नहीं पायी जाती। कहीं दिशानिर्देश मौजूद हैं, तो उद्देश्य निर्धारित नहीं हैं। कहीं उद्देश्य निर्धारित हैं, तो दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं। कहीं दिशानिर्देश और उद्देश्यों को कुछ हद तक परिभाषित किया गया है तो, उसमें वह उच्चता और उत्कृष्टता नहीं है जो कि इस्लाम की विशिष्ट विशेषता है। अतः यह तथ्य आज सर्वथा निर्विवाद है कि युद्ध को उसकी प्राकृतिक सीमा के भीतर सीमित करने और उसे एक बर्बर संघर्ष से सभ्य प्रतिस्पर्धा तक और अत्याचार से न्याय के स्तर तक और बुराई से अच्छाई और दायित्व के स्तर तक लाने की अगर किसी ने कोशिश की है, तो वह केवल इस्लाम है। इस नियम को अपनाकर संसार को अत्याचार के अभिशाप से भी बचाया जा सकता है और दमन के अभिशाप से भी।
अध्याय सात
आधुनिक सभ्यता में युद्ध
इस अध्याय में हम वर्तमान सभ्यता में युद्ध के उद्देश्यों और युद्ध के नियमों की जांच कर यह देखना चाहते हैं कि नैतिकता और मानवता के मामले में उनकी स्थिति क्या है। हमारी पिछली बहसों को देखकर कोई कह सकता है कि “यह सच है कि इस्लाम ने अपने युग की सभ्यता में बहुत सुधार किया और उसने युद्ध के ऐसे उद्देश्यों और तरीक़ों की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन किया जिससे उसकी समकालीन सभ्यताएँ और धर्म अपरिचित थे, लेकिन आज, सदियों के विकास के बाद युद्ध के बारे में मानवीय विचारों में जो परिपक्वता आई और उसके आधार पर जो क़ानून अस्तित्व में आए हैं, इन से उस युग के क़ानूनों और विचारों का क्या मुक़ाबला हो सकता है? इसलिए एक और तुलना की ज़रूरत है जिसमें इस्लाम और आधुनिक सभ्यता को आमने-सामने रख कर देखा जाए कि युद्ध से संबंधित किसके लक्ष्य और तरीक़े अधिक सही, अधिक उपयोगी और अधिक मज़बूत हैं।
इस तुलना को शुरू करने से पहले, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि युद्ध के संबंध में पश्चिमी सभ्यता के मूल क़ानून का पता लगाने के लिए हमें किस चीज़ की ओर जाना चाहिए। किसी विषय में किसी मानव समूह की मान्यताओं और व्यवहारों की स्थिति का पता सामान्यतः तीन बातों धर्म, साहित्य और समाज के व्यवहार से चलता है। जहां तक धर्म का संबंध है,तो आधुनिक सभ्यता ने इसे व्यक्ति का निजी मुद्दा बना दिया है और सभ्य जीवन के मामलों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जहां तक साहित्य का संबंध है, निस्संदेह पश्चिम में उनका एक विशाल संग्रह मौजूद है। पश्चिमी विद्वानों और विचारकों ने युद्ध और युद्ध से जुड़े विषयों पर बहुत कुछ लिखा है और हर पहलु से उसपर बहस की है। इन विद्वानों के विचारों का सामूहिक विचारों के विकास में चाहे कितना ही प्रभाव क्यों न हो और समाज के क़ानून निर्माण में उनके विचारों ने चाहे कितना ही योगदान क्यों न दिया हो, मगर उनके पास स्वयं के भीतर कोई ऐसी शक्ति नहीं होती है, जिसके आधार पर उन्हें मानव जाति के लिए एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सके। यहां तक कि दुनिया के बड़े से बड़े लेखक को भी यह गौरव प्राप्त नहीं है कि उसका कोई कथन उसकी पूरी जाति के लिए क़ानून का दर्जा रखता हो। यह ज़रूर हो सकता है कि उनकी बातों से प्रभावित होकर उनके समुदाय ने अपने लिए कई क़ानून बना लिए हों, लेकिन वे क़ानून इस तर्क से उस जाति पर बाध्यकारी नहीं होंगे कि वे अमुक लेखक के कथन हैं, बल्कि इस आधार पर होगा कि राष्ट्र ने उसे अपने लिए एक क़ानून के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः युद्ध के विषय पर पश्चिमी विद्वानों के बहुमूल्य प्रयत्नों द्वारा पश्चिमी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया विशाल साहित्य संग्रह हमारे लिए अनुपयोगी है। अब केवल तीसरी चीज़ रह जाती है, जिससे हम पाश्चात्य सभ्यता में युद्ध के लक्ष्यों और उद्देश्यों का पता लगा सकते हैं और वह है पश्चिमी राष्ट्रों की अंतःक्रिया। यह अंतःक्रिया दो प्रकार की है। एक संहिताबद्ध या लिखित, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क़ानून कहा जाता है। दूसरा अलिखित है जो राज्यों के आपसी मामलों और व्यावहारिक राजनीति को संदर्भित करता है। इन दोनों में से कौन सा क़ानून अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक है? विरोधाभास की स्थिति में किस पर भरोसा किया जाएगा? और पश्चिमी राष्ट्रों के लिए प्रमाण बनने की असली क्षमता किसके पास है? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पश्चिमी विद्वानों में भारी असहमति है और आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। लेकिन हमें इस सैद्धान्तिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, यह मुद्दा युद्ध के दो पहलुओं के बीच कुछ हद तक विभाजित हो गया है, जैसे कि युद्ध का नैतिक पहलू अलिखित क़ानून के दायरे में आ गया है और व्यावहारिक पहलू पर लिखित क़ानून का प्रभुत्व हो गया है। इसलिए, हम प्राथमिकता के प्रश्न को छोड़कर, दो पहलुओं पर अलग-अलग चर्चा करेंगे।
युद्ध का नैतिक पहलू
युद्ध के विषय की खोज में अब तक हमने जिस पद्धति का अनुसरण किया है, उसके अनुसार युद्ध का नैतिक पहलू क्रम में सबसे पहले आता है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पश्चिमी सभ्यता युद्ध को किस दृष्टि से देखती है। उसकी नैतिकता की प्रणाली में युद्ध की स्थिति क्या है? उसके अनुसार युद्ध किन उद्देश्यों के लिए अनुमन्य है और किसके लिए यह नाजायज़ है? अगर इस दृष्टि से उसका कोई उच्च और शुद्ध आदर्श है तो वह क्या है? और अगर ऐसा नहीं है, तो नैतिकता और सभ्यता की दुनिया में इसका क्या स्थान है? इन सवालों को हल करने के वाद युद्ध के क़ानून के उचित और अनुचित होने के सवाल पर चर्चा की जाएगी।
उपरोक्त प्रश्नों पर पश्चिमी संहिताबद्ध क़ानून पूरी तरह से मौन है। शुरुआती समय में नैतिकता के सवाल को अंतरराष्ट्रीय क़ानून में एक प्रासंगिक सवाल माना जाता था। इसलिए, इस क़ानून के पहले लेखक ग्रोटियस ने अपनी किताब (बी ज्यूर बेलियाक पैकिस) में कई स्थानों पर युद्ध के वैध और अवैध उद्देश्यों के बीच अंतर करने की कोशिश की है। लेकिन आधुनिक युग के अंतरराष्ट्रीय क़ानून ने इस प्रश्न को चर्चा से पूरी तरह बाहर कर दिया है। प्रोफ़ेसर लारेंस अपनी किताब “प्रिंसिपल्स ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ” में लिखता हैं:
“लेकिन आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क़ानून इन नैतिक सवालों के बारे में कुछ नहीं जानता। यह उन पर कुछ नहीं बोलता है, बल्कि यह उनकी पूरी तरह अनदेखी करता है। उसके लिए युद्ध, चाहे वह न्यायोचित हो या अन्यायपूर्ण, सही हो या ग़लत, एक ऐसा तथ्य है जो विभिन्न प्रकार से संबंधित पक्षों के संबंधों को बदल देता है। इसलिए, क़ानून का काम यह है कि इसे परिभाषित करे और इस परिवर्तन की सीमाओं और क़ानूनी घटनाओं को निर्धारित कर दे। क़ानून हमें यह बताएगा कि आयोधन (belligerency) का संबंध कैसे बनता है, और एक दूसरे के प्रति और तटस्थों के प्रति योद्धा के अधिकार और दायित्व क्या हैं; लेकिन हम उन नैतिक सवालों पर मार्गदर्शन के लिए नैतिक चर्चाओं की ओर देखते हैं जो शुरुआती प्रचारकों के लेखन में इतना बड़ा स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रोटियस, युद्ध के उचित कारणों को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है, यह तय करने के बाद कि युद्ध आवश्यक रूप से ग़लत नहीं है, मुख्य रूप से इसे 'मृत्युदंड' के साथ भ्रमित करने की प्रक्रिया से। ^ इस तरह के प्रश्न सबसे सावधानीपूर्वक विचार के योग्य हैं; लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर एक ग्रंथ में उतनी ही अप्रासंगिक हैं जितनी कि व्यक्तिगत स्थिति के क़ानून पर एक किताब में शादी की नैतिकता पर चर्चा होगी।” (लारेंस “प्रिंसिपल्स ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ” पी. 292)
एक जर्मन लेखक, एलिज़बैकर लिखता है:
“अंतर्राष्ट्रीय क़ानून ने हमेशा युद्ध के कार्यों पर केवल ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जो युद्ध के उद्देश्यों में सराहनीय हस्तक्षेप के बिना देखे जा सकते हैं। इसने ख़ुद को यह निर्धारित करने के साथ संतुष्ट किया है कि जहां तक संभव हो दुश्मन को अनावश्यक नुक़सान से छूट दी जानी चाहिए। ऐसी क्षति पहुँचाने से परहेज़ किया जाए जो किसी भी तरह से युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं या उस की तुलना में बहुत महंगी हैं।”
प्रोफेसर नेपोल्ड लिखते हैं:
इसलिए, युद्ध में अपराध का प्रश्न अंतरराष्ट्रीय क़ानून का प्रश्न नहीं है, बल्कि नैतिकता का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय क़ानून वैध और अवैध युद्ध के बीच अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध को हमेशा अंतरराष्ट्रीय क़ानून के दृष्टिकोण से क़ानून का उल्लंघन माना जाता है। (निप्पोल्ड, विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का विकास, एल्ट्ज़बैकर निप्पोल्ड. पीपी. 7-8)
इससे पता चलता है कि जहां तक लिखित या संहिताबद्ध अंतरराष्ट्रीय क़ानून का संबंध है, तो इसमें सही और ग़लत, वैध और अवैध युद्ध के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। इससे हम यह नहीं जान सकते कि पश्चिमी सभ्यता किन उद्देश्यों के लिए युद्ध को जायज़ रखती है और किन प्रयोजनों के लिए नाजायज़? लेकिन जैसा कि डॉ बाई ने कहा है, “एक अंतरराष्ट्रीय क़ानून अलिखित भी है, और वास्तविक क़ानून वही है।” इसलिए, अब हमें यह देखना होगा कि पश्चिम के सबसे सभ्य राष्ट्रों ने इस संबंध में क्या किया है। वे राष्ट्र जिनके कार्य आधुनिक सभ्यता के मानक और आदर्श हैं, जिनकी गतिविधियों को सभ्यता का दर्जा प्राप्त है और जिनके कथन और कर्म के सिवा किसी और चीज़ को आधुनिक सभ्यता के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जब उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है, तो किन उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए होता है और क्या उनके बीच इस प्रकार के युद्ध को सत्य और न्याय का युद्ध कहा जाता है। इसके लिए हम उन छोटी-छोटी लड़ाइयों की चर्चा नहीं करेंगे जो उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में सभ्य और (पश्चिमी दृष्टिकोण से) असभ्य राष्ट्रों के एक छोटे समूह के बीच हुई थीं। क्योंकि इनमें जो हुआ, उसे हम पश्चिमी सभ्यता का पूरा मॉडल नहीं कह सकते। उन सब को छोड़कर हम केवल 20वीं शताब्दी के उस महायुद्ध पर नज़र डालते हैं, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के सभी अग्रदूत शामिल थे। या दूसरे शब्दों में, जिसकी कार्यकारिणी परिषद में आधुनिक विश्व के सभी सभ्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व था। इस युद्ध का हाल हमें बता सकता है कि पश्चिमी सभ्यता की दृष्टि में वैध और अवैध युद्ध के बीच अंतर करने का नैतिक मानक क्या है।
महायुद्ध (प्रथम) के कारण:
1914-18 का महायुद्ध मूल रूप से छह प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, हालांकि अन्य छोटे राष्ट्र भी उसमें शामिल हो गए थे। एक पक्ष में जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे, और दूसरे में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली शामिल थे। ये दो प्रतिद्वंद्वी समूह जिन राष्ट्रों से बने थे, उनमें तीव्र और ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी। इंग्लैंड फ्रांस का पुराना दुश्मन था, 1899 में सूडान के मुद्दे पर उसका युद्ध होते-होते रह गया था। रूस और इंग्लैंड के बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता थी, यहां तक कि 20वीं सदी की शुरुआत तक, भारत पर रूसी आक्रमण का ख़तरा अंग्रेज़ी साम्राज्य को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखता था। फ़्रांस और इटली के बीच ट्यूनीशियाई मुद्दा लगभग आधी शताब्दी के लिए प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता का स्रोत रहा था, और विश्वयुद्ध की शुरुआत तक जर्मनी के साथ इटली का गठबंधन बना हुआ था। लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में इन शत्रु राष्ट्रों के बीच कुछ सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य पैदा हुए, जिसके कारण ये सभी एकजुट हो गए और दूसरे समूह के ख़िलाफ़ युद्ध में भाग लिया। दूसरी ओर, जर्मनी 1904 तक इंग्लैंड का मित्र था, 1914 तक इटली के साथ उसका संबद्ध था, रूस 1908 तक उसका मित्र था, बल्कि युद्ध की शुरुआत तक ज़ार और कैसर के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन कुछ अन्य मक़सद भी थे, जिन्होंने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, और जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ एकजुट होकर अपने इन प्राचीन दोस्तों के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा, जो कभी उसके सहयोगी रह चुके थे।
राष्ट्रों की जत्थेबंदी:
ये विशेष उद्देश्य क्या थे? धर्म का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि सभी ईसाई थे, मातृभूमि की रक्षा का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि किसी ने किसी पर हमला नहीं किया था। अधिकारों का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि हर कोई अपने अधिकारों का पूरा आनंद ले रहा था। फिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए प्रेरित किया? इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि यह और कुछ नहीं था कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हिस्से से अधिक लेना चाहता था, और प्रत्येक पक्ष की इच्छा दूसरे पक्ष को दबा कर या उसका सफ़ाया करके उसके लाभों को अपने पक्ष में करने की थी।
उनके बीच दुश्मनी का पहला बीज 1870 में पड़ा था जब जर्मनी ने फ्रांस से अल्सेस और लोरेन छीन लिया था। हालाँकि अल्सेस की पूरी आबादी जर्मन मूल की थी और लोरेन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जातीय और भाषाई रूप से जर्मन था, फिर भी फ्रांस ने उसे अपने राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन माना और उस समय से यह फ्रांसीसी राजनीति का प्रमुख लक्ष्य बन गया कि वह जर्मनी को नीचा दिखाकर उन प्रांतों को फिर से हासिल कर ले।
उसके बाद, जर्मन व्यापार और उद्योग का विकास शुरू हुआ, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक वह दुनिया के महान औद्योगिक और वाणिज्यिक राष्ट्रों में से एक बन गया। 1900 के दशक में, उसने महसूस किया कि इंग्लैंड समुद्री व्यापार के सभी संसाधनों पर हावी है और एक शक्तिशाली युद्ध बेड़े के बिना इस प्रभुत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः उसने अपनी नौसैनिक शक्ति का तेज़ी से विकास करना शुरू कर दिया। इस बढ़ते खतरे को इंग्लैंड ने महसूस किया। पहले उसने जर्मनी से दोस्ती करने की कोशिश की। 1899 से 1902 तक, मेसर्स गिबरलेन, लॉर्ड लांस डाउन और अन्य ब्रिटिश बुद्धिजीवियों ने इस पर काम करना जारी रखा। लेकिन जर्मनी ब्रिटेन की नौसैनिक और वाणिज्यिक श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और विश्व व्यापार में प्रमुख शक्ति बनना चाहता था, इसलिए दोनों प्रतिद्वंद्वी सहयोगी नहीं बन सके और विश्व राजनीति में अचानक एक क्रांति आ गई। इस क्रांति की पहली झलक 1904 में मिली थी, जब सदियों पुराने दुश्मन इंग्लैंड और फ्रांस ने एक-दूसरे को गले लगा लिया। फ्रांस ने मिस्र पर ब्रिटिश क़ब्ज़े को मान्यता दे दी। जवाब में, इंग्लैंड ने मोरक्को के फ्रांसीसी क़ब्ज़े को मान्यता दी और दोनों देशों ने एकजुट होकर अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए एक समझौता कर लिया।
उसके बाद 1907 में रूस भी इस समूह में शामिल हो गया। उसके सामने दो बड़े लक्ष्य थे। डैनियल पास और बोस्फोरस पर क़ब्ज़ा, जिसके लिए वह डेढ़ सौ वर्षों से प्रयास कर रहा था। दूसरा बाल्कन प्रायद्वीपों पर हावी होना ताकि ईजियन और भूमध्य सागर तक उसे पहुंच प्राप्त हो सके । इन दोनों उद्देश्यों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया उसके प्रतिद्वंद्वी थे। जर्मनी बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे लाइन स्थापित करके अपने पूर्वी व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था, जिसके लिए वह चाहता था कि तुर्की और बाल्कन रूसी प्रभाव से मुक्त रहें। दूसरी ओर, ऑस्ट्रिया को साम्राज्य के विस्तार और व्यापार विस्तार की अपनी लालसा को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीक़ा यही दिखाई दिया कि बाल्कन प्रायद्वीप पर क़ब्ज़ा करके एजियन और एड्रियाटिक बंदरगाहों का लाभ उठाए। इसलिए, इस उद्देश्य के लिए, उसने 1908 में बोस्निया और हर्जेगोविना पर औपचारिक रूप से क़ब्ज़ा कर लिया। 1907 तक, इंग्लैंड रूस के राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण बना रहा। लेकिन जब उसने महसूस किया कि रूस की मदद के बिना वह जर्मनी का गला घोंटने में सफल नहीं हो सकता है, तो उसने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसे आश्वासन दिया कि वह डैनियल और बोस्फोरस पर क़ब्ज़ा करने में उसकी मदद करेगा।
इस तरह 1907 तक दो ज़बरदस्त गुट बन गए। एक गुट में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, दूसरे में जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे। पहले गुट वालों के बीच एकजुटता का कारण यह था कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने और दुनिया के वाणिज्यिक और आर्थिक जीवन पर हावी होने के इच्छुक थे। इटली अभी तक इस वर्गीकरण में पूरी तरह शामिल नहीं था। ज़ाहिर तौर पर वह जर्मनी के साथ एक संधि गठबंधन से जुड़ा था। लेकिन किसी तरह वह अपने जर्मन मित्र को छोड़कर फ्रांसीसी शत्रु में कैसे शामिल हो गया? यह एक अजीब कहानी है। इटली ने पाँचों शक्तियों के साथ अपने संबंधों और संधियों को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि वह जब उसे ट्यूनिस पर क़ब्ज़ा करने के लिए फ्रांस के ख़िलाफ़ युद्ध की ज़रूरत हो तो जर्मनी से सहायता का दावा कर सके, और जब ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्रों (जिन पर इटली का लंबे समय से दबदबा था) ) अगर युद्ध की ज़रूरत पड़ी तो उसे मित्र राष्ट्रों की सहायता मिल सके। महायुद्ध की शुरुआत में, जब उसने देखा कि इंग्लैंड की महान नौसैनिक शक्ति फ्रांस के साथ थी, और फ्रांस से ट्यूनीशिया के क्षेत्र को जीतने में जर्मनी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो वह तुरंत मित्र राष्ट्रों की ओर मुड़ गया। दक्षिणपंथ ने दावा करना शुरू कर दिया कि हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया को झूठा मानते हैं और इसलिए उनका समर्थन नहीं कर सकते।
युद्ध की शुरुआत
जून 1914 में जब एक सर्बियाई अराजकतावादी द्वारा ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस की हत्या कर दी गई, तो साज़िश और बिगाड़ की फ़सल, जो 44 वर्षों से बोई और सिंची जा रही थी, पक कर कटने को एक़दम से तैयार हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्वियन रोड़े को हटाने के लिए इस अवसर को उचित समझा, जो बाल्कन की ओर बढ़ने में रुकावट था। जर्मनी ने भी सर्बिया के अंत को अपनी व्यापारिक योजना की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता था, अत: वह भी ऑस्ट्रिया का सहयोगी बन गया। दूसरी ओर, रूस सर्बिया को अपना “छोटा भाई” मानता था और बाल्कन में उसकी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हुई थीं, और यह भी तय था कि अगर ऑस्ट्रिया सर्बिया का अंत करने में सफल हो गया, तो बाल्कन पर उसके प्रभुत्व को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वह अपने छोटे भाई के समर्थन में खड़ा हो गया। दूसरी ओर फ्रांस को ख़तरा था कि रूस और सर्बिया को जीतकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसे अल्सेस और लोरेन को वापस लेना तो दूर, ख़ुद पेरिस पर क़ब्ज़ा बनाए रखना असंभव हो जाएगा। इसलिए, वह भी रूस का समर्थन करने के लिए तैयार हो गया। इन सहयोगियों के बाद, इंग्लैंड के लिए अलग रहना असंभव था। उस ने अपने ऊपर कई नैतिक जिम्मेदारियाँ ले रखी थीं, जिनके निष्पादन के लिए आवश्यक था कि नौसैनिक और व्यापारिक वर्चस्व के रास्ते से जर्मनी के बढ़ते ख़तरे को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। इसलिए वह भी हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ और दुनिया में “सभ्य राष्ट्रों” का वह महायुद्ध शुरू हुआ जिसके सामने पिछले असभ्य राष्ट्रों की लड़ाइयां नगण्य हो कर रह गईं।
युद्ध के भागीदारों के लक्ष्य और उद्देश्य
युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक राष्ट्र का दावा था कि उसे अपने “पवित्र” अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध पर मजबूर होना पड़ा है। और केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य कमज़ोर राष्ट्रों को “आज़ादी” दिलाने के लिए, और दमन और हिंसा की ताक़तों को पराजित कर के, दुनिया में न्याय और शांति की स्थापना के लिए। लेकिन युद्ध के दौरान और युद्ध की समाप्ति के बाद, उन “सत्य और न्याय के ठेकेदारों” ने जिस तरह राष्ट्रों और देशों का लेन-देन किया और साम्राज्यों की बांट और क्षेत्रों के विभाजन का व्यवसाय जिस व्यापक पैमाने पर किया, उसकी स्थिति को देखकर मालूम हो जाता है कि पश्चिमी सभ्यता में “सत्य और न्याय” किस चीज़ का नाम है।
1917 में, ऑस्ट्रिया, हंगरी के राजा कार्ल ने कोशिश की थी कि अपने सहयोगियों से अलग होकर इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के साथ अलग से संधि कर ले। इस उद्देश्य के लिए उसने बोरबॉन के प्रिंस सिक्सते के माध्यम से सहयोगियों के साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की थी, और उस वार्ता की सभी विवरण को राजकुमार ने ख़ुद लिखा था, जो बाद में “ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव” के नाम से प्रकाशित हुआ। उस वार्ता विवरण के अध्ययन से उस व्यापार की पूरी प्रकृति का पता चलता है जो देशों और राष्ट्रों के रूप में किया जा रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड ने इटली को इस वादे के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए राजी किया था कि ऑस्ट्रिया का दक्षिणी हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। इस विभाजन के कारण इटली ने ऑस्ट्रिया के साथ अलग शांति का विरोध किया। फ्रांस विशेष रूप से चाहता था कि ऑस्ट्रिया जर्मनी से अलग हो जाए, इसलिए उसने इटली पर शांति स्वीकार करने के लिए बहुत दबाव डाला। लेकिन इटली ने इसका इतना घोर विरोध किया कि मित्र राष्ट्रों को यह भी डर होने लगा था कि कहीं वह “सत्य” का साथ छोड़कर “असत्य” (अर्थात् जर्मनी) के साथ न मिल जाए। एम. पॉल कोम्बेउ, जो उस समय लंदन में फ्रांस का राजदूत था, प्रिंस सिकस्ते के साथ एक मुलाकात के दौरान कहता है कि:
“इटली का लालच उसे हर तरह की बदमाशियों की ओर ले जा सकता है।” (ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव, पी.103)
एक अन्य बैठक में उसने कहा कि:
“इटली ने बार-बार घोषित किया है कि वह केवल उन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए युद्ध में शामिल हुआ है जिन्हें वह ऑस्ट्रिया से प्राप्त करना चाहता था।(ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव, पृष्ठ 173)
पॉल कोम्बेउ के भाई, एम. ज़ौल कोम्बेउ, जो पहले बर्लिन में फ्रांसीसी राजदूत था, इस आधार पर वार्ता का विरोध करता है कि:
“अगर ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली गई, तो निस्संदेह इस संधि पर हस्ताक्षर करने के 48 घंटों के भीतर वेरेब जर्मनी की बाहों में होगा।” (ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव, पृ.28)
एक अन्य अवसर पर वह कहता है:
इटली हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। वह केवल एक ही विचार रखता है और वह यह है कि युद्ध के बाद जब दूसरे साथी थक कर चूर हो चुके होंगे तो वह आर्थिक गतिविधियों में अपने साथियों से आगे निकलने की कोशिश करे।” (ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव, पृ.173)
ये उन “सत्य और न्याय के ध्वजावाहकों” के आंतरिक उद्देश्य थे। और यह ख़ुद उन लोगों की एक दूसरे के बारे में राय थी जो “सत्य और न्याय” के लिए एक साथ लड़ रहे थे। अंत में, जब यह स्पष्ट हो गया कि इटली एक विस्तारित साम्राज्य के इरादों को छोड़कर, ऑस्ट्रिया के साथ संधि करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके सत्य और न्याय के ध्वजावाहक “सहयोगियों” ने ऑस्ट्रिया से कहा कि तुम उन क्षेत्रों को इटली के लिए छोड़ दो, जिनकी उसे लालच है, और बदले में हम तुम्हें जर्मनी से छीन कर सिलेसिया और बवेरिया के इलाक़े दिलवा देंगे। जैसा कि सर्वविदित है, इन दो प्रांतों में विशेष जर्मन मूल के लोग रहते हैं और जर्मन मातृभूमि के अभिन्न अंग हैं, लेकिन “सत्य और न्याय के ध्वजावाहक” सहयोगी उन्हें ऑस्ट्रिया को इस तरह सौंपने को तैयार थे जैसे कि वे उनके ही इलाक़े हों। और मजे की बात यह है कि “सत्य और न्याय के ध्वजावाहक” ऑस्ट्रिया ने भी उन्हें स्वीकार करने से इस आधार पर इंकार नहीं किया कि वे उसके मित्र जर्मनी के क्षेत्र थे, बल्कि केवल इसलिए कि वे वर्तमान में एक फ्रांस की जायदाद नहीं थे, और उन्हें संदेह था कि फ्रांस के पास उन्हें छीन कर उसे सौंपने की शक्ति है। उसके बाद कुछ और इलाक़ो की तलाश शुरू हुई ताकि उन्हें ऑस्ट्रिया को सौंपकर उसके नुक़सान की भरपाई की जाए। पहले त्रिपोली पर नज़र डाली गई, लेकिन इटली ने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि यह प्राचीन रोमन साम्राज्य का सपना देख रहा था। और इसके लिए उसे कर्टाजिना (कोलम्बिया) का पूरा क्षेत्र उसे चाहिए था। फिर इरिट्रिया और सोमालीलैंड पर नज़र गई। इन दोनों क्षेत्रों में इटली की विशेष रुचि नहीं थी और ऑस्ट्रिया भी इन्हें स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन कुछ कारणों से यह मामला भी नहीं निपट सका और इटली के लालच के कारण मित्र राष्ट्रों के साथ ऑस्ट्रिया की शांति वार्ता कट गई। (ऑस्ट्रिया का शांति प्रस्ताव, पृ.139)
गोपनीय समझौते
इस व्यवसाय के वृत्तांत में एक और अध्याय उन गुप्त संधियों का है, जो युद्ध के दौरान मित्र देशों के बीच हुई थीं। अगर युद्ध के दौरान रूस क्रांति का शिकार नहीं हुआ होता तो अंतरराष्ट्रीय डकैती की यह योजना शायद गुप्त ही रह जाती। 1917 में, जब tsarist सरकार को उखाड़ फेंका गया और बोल्शेविक सत्ता में आए, तो उन्होंने पूंजीपतियों को बेनकाब करने के लिए tsarist सरकार के गुप्त कक्षों से प्राप्त सभी गुप्त समझौतों को प्रकाशित कर दिया। इस प्रकार, उन “सभ्य” राष्ट्रों की घृणित कूटनीति अचानक पूरी दुनिया के सामने आ गई। उन संधियों में ऐसा कोई खंड नहीं था जिसमें “सत्य और न्याय के ध्वाजावाहकों” ने विरोधी साम्राज्य के किसी न किसी क्षेत्र या उनके आर्थिक धन के कुछ स्रोत को आपस में बांटने का निर्णय नहीं किया हो।
प्रारंभिक निर्णय यह था कि अल्सेस और लोरेन को फ्रांस में मिला लिया जाएगा, हालांकि उन दो प्रांतों में ज़्यादातर जर्मन वंश के लोग रहते थे और भौगोलिक रूप से वे फ्रांस की तुलना में जर्मनी से अधिक निकट थे। लेकिन उन्हें केवल इस आधार पर फ़्रांस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था कि वे 1870 से पहले फ़्रांस के क़ब्ज़े में थे। दूसरे, यह निर्णय लिया गया कि राइन नदी के पश्चिम के सभी जर्मन क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को फ्रांस और रूस ने अपने सहयोगी इंग्लैंड से भी गुप्त रखा था, और यह तब व्यक्त किया गया था जब युद्ध की समाप्ति के बाद शांति परिषद में युद्ध की लूट का विभाजन शुरू हुअ। तीसरा फ़ैसला यह था कि मोरक्को को, जो अब तक फ्रांसीसी नेतृत्व में था, प्रांस द्वारा क़ब्ज़े में लिया हुआ स्वीकार किया जाएगा। सभी जर्मनी के सारे क़ब्ज़े भी फ्रांस के हिस्से में आएंगे और तुर्की में से भी उसे बड़ा हिस्सा दिया जाएगा।
यह तो था “सत्य और न्याय के ध्वजावाहक” फ्रांस का हिस्सा। इटली को भी संतुष्ट करना आवश्यक था, क्योंकि वह केवल “सत्य और न्याय” के लिए “असत्य” का साथ छोड़कर युद्ध में शामिल हुआ था। उसके लिए टार्टिनो, ट्राएस्टे और दक्षिण टायरॉल के क्षेत्र अलग किए गए, एड्रियाटिक के पूरे तट और द्वीप भी उसके हिस्से में आए, और तुर्की के बहुत से क़ब्ज़े भी उसे देने का वादा किया गया।
रूस में सत्य और न्याय का सबसे बड़ा ध्वजावाहक ज़ार शासक था। यह कैसे संभव था कि इस व्यवसाय में उसका हिस्सा उसकी “सत्य और न्याय” के योग्य नहीं होता ? उसके साथ पहला समझौता पोलैंड से संबंधित था, जिसका सारांश यह था कि पोलिश राष्ट्र की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए रूस को हर संभावित कार्रवाई करने का अधिकार है। यह वही पोलैण्ड है जिसे युद्ध के प्रारम्भ में स्वतंत्रता की आशा दिलाई गयी थी और युद्ध की समाप्ति पर बोल्शेविकों की हठधर्मिता के कारण जिसके समर्थन का दायित्व फ्रांस ने और फिर इंग्लैण्ड ने ले लिया। दूसरी संधि कांस्टेंटिनोपल और जलडमरूमध्य के बारे में थी। फरवरी 1914 में, युद्ध शुरू होने से छह महीने पहले, रूस के क्राउन कौंसिल ने यह फ़ैसला कर लिया था कि डेनियल पास और बोस्फोरस के विलय में देरी करना अब उचित नहीं है। अतः इस उद्देश्य के लिए युद्ध की तैयारियाँ भी प्रारम्भ कर दी गयी थीं। फिर, जब महायुद्ध छिड़ गया, तो रूस ने सबसे पहले अपने “नैतिक दायित्व” को पूरा करने के बारे में सोचा और 1915 की गुप्त समझौता में, उसने अपने सहयोगियों से यह स्वीकार करा लिया कि युद्ध की लूट में से उसे डैनियल, बोस्फोरस पास, कांस्टेंटिनोपल और एशिया माइनर का पूर्वी भाग ज़रूर दिया जाए। एक रूसी इतिहासकार बैरन एस.ए. कर्फ़ (1922) लिखता है:
“इस गुप्त समझौते के अनुसार, ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया-हंगरी को युद्ध की लूट ठहराया गया, जिन्हें मित्र राष्ट्रों में विभाजित करने का फ़ैसला कर लिया गया। इस विभाजन में, कांस्टेंटिनोपल और डैनियल और बोस्फोरस के जलडमरूमध्य को निश्चित रूप से रूस को सौंपा गया था।”
अब रह गया इंग्लैंड, जो “सत्य और न्याय के सभी ध्वाजावाहकों” का नेतृत्व कर रहा था। अतः उसने जर्मनी के अफ्रीकी और एशियाई उपनिवेशों को अपने लिए पर्याप्त न मानकर एक अन्य क्षेत्र का निर्माण किया जो उसकी वीरता के योग्य था। युद्ध की घोषणा के पांच महीने बाद मार्च 1915 में, उसने फ्रांस के साथ एक प्रारंभिक गुप्त समझौता किया जिसने अरब दुनिया को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। एक क्षेत्र सीरिया था, दूसरा क्षेत्र इराक़ था, पहल क्षेत्र को फ्रांसीसी प्रभाव के तहत मान्यता दी गई, और दूसरे क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार स्थापित किए गए। इस विभाजन की सफलता इसके बिना संभव न थी कि ख़ुद अरब वाले इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ बटाते, और अरबों के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वे अपने देश के विभाजन के रहस्य से अवगत होने के बाद उसकी विजय में ख़ुद शत्रुओं के सहायक बनना स्वीकार कर लेते। इसलिए यह चाल चली गइ कि विभाजन के प्रारंभिक समझौते को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और अरबी नेताओं को यह विश्वास दिलाया गया कि अगर उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर अरब में तुर्की सरकार को उखाड़ फेंका, तो उसके बदले, एक स्वतंत्र अरब राज्य स्थापित किया जाएगा जो दक्षिणी इराक़ और लेबनान की तटीय पट्टी को छोड़ कर पूरे अरब पर फैला होगा।
आज़ादी के इस सुखद सपने ने अरबों में एक नई भावना जगा दी और अक्टूबर 1915 में (यानी ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच गुप्त समझौते के 9 महीने बाद), उन्होंने सर हेनरी मैकमोहन के माध्यम से मित्र राष्ट्रों के साथ एक संधि कर ली, जिसके द्वारा उनकी पूरी ताक़त दो सहयोगियों के साथ हो गई। इस सहायता के बदले में उन्हें एक कागजी समझौता प्राप्त हुआ कि युद्ध की समाप्ति के बाद अरब देशों को एक स्थायी साम्राज्य बना दिया जाएगा। इस समझौते के बाद जून 1916 में शरीफ हुसैन ने तुर्की के ख़िलाफ़ विद्रोह की घोषणा कर दी। धीरे-धीरे इराक़, सीरिया और फ़िलिस्तीन में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। कुछ ही महीनों में यह निश्चित हो गया कि तुर्की सत्ता अब अरब देशों में नहीं रह पाएगी और ब्रिटेन व फ्रांस के संयुक्त लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए, नवंबर 1916 में, दोनों साम्राज्यों ने फिर से बातचीत की और एक और गुप्त समझौता किया गया, जिसे साइक्स-पिकोट समझौते के रूप में जाना जाता है। इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि इराक़ पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। सीरिया पूरी तरह से फ्रांसीसी साम्राज्य के अधीन हो जाएगा। फ़िलिस्तीन एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र होगा और हाइफ़ा, अपने बंदरगाह सहित, ब्रिटिश प्रभाव में रहेगा। शेष रहे वे देश जो इराक़ और सीरिया के तट के बीच स्थित हैं, तो उन को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक ब्रिटेन के प्रभाव में होगा और दूसरा फ्रांस के प्रभाव में होगा।
इस संधि में अंग्रेज़ प्रतिनिधि सर मार्क साइक्स ने मोसुल को फ्रांसीसी प्रभाव में सौंपने पर सहमति व्यक्त कर ली थी। क्योंकि इससे पहले 1915 के एक गुप्त समझौते से यह तय हो गया था कि आर्मेनिया, पूर्वी कुर्दिस्तान और मोसुल की सीमा से सटे तुर्की के इलाक़े रूस को दे दिए जाएंगे और ब्रिटिश नीति की मांग थी कि उसकी सीमा रूस से न मिलने पाए। इसलिए उसने रूस के पड़ोस के राजनीतिक ख़तरों से बचने के लिए ब्रिटिश और रूसी क्षेत्रों के बीच एक फ्रांसीसी क्षेत्र रखना उचित समझा। लेकिन मोसुल के तेल के कुओं पर शुरू से ही ब्रिटेन की नज़र थी, इसलिए जब रूस का ख़तरा नहीं रहा, तो उसने आख़िरकार फ्रांस की दोस्ती की परवाह किए बिना उसे प्राप्त करके छोड़ा।
युद्ध के बाद देशों का विभाजन
ये वे इरादे और योजनाएँ थीं जिनके साथ सत्य और न्याय के ध्वजावाहक “पश्चिमी राष्ट्रों” ने युद्ध में प्रवेश किया था। आइए देखें कि युद्ध के बाद उन्होंने अपनी “सत्यता और न्यायप्रियता” को कैसे साबित किया।
युद्ध के अंतिम दिनों में दो घटनाएँ सी घटीं जिन्होंने 1915 और 1917 के बीच गुप्त संधियों द्वारा स्थापित मानचित्र को बहुत कुछ बदल दिया। उनमें से एक घटना थी अमेरिका का युद्ध में शामिल होना और दूसरी थी रूसी क्रांति। यूरोप के मामलों से अलग-थलग रहने की प्राचीन नीति को त्यागकर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि वह अपने व्यापार की सफलता के लिए शांति चाहता था, इसलिए उसका पूरा प्रयास था कि युद्ध के बाद युद्ध की लूट के बटवारे को लेकर ऐसा असंतुलन न पैदा हो जो एक और युद्ध की ओर ले जाए। दूसरी ओर, रूस ने जिस शाही सरकार के तहत युद्ध में भाग लिया था, 1917 के अंत में उसका तख़्ता पलट हो गया और उस पर बोल्शेविक पार्टी को वर्चस्व हासिल हो गया, जो इंग्लैंड, फ्रांस और इटली, के हितों के लिए जर्मनी की तुलना में अधिक ख़तरनाक थी। इसलिए युद्ध की लूट की बन्दरबांट में रूस का जो हिस्सा निर्धारित किया गया था, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, और सत्य और न्याय के ध्वजावाहक “मित्र राष्ट्रों” को एक नया नक्शा तैयार करना पड़ा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की शांतिप्रिय भावनाओं का मान रखना भी आवश्यक था ।
“सत्य और न्याय” का यह प्रदर्शन तो यूरोप में किया गया। अब एशिया पर नज़र डालते हैं, कि “सत्य और न्याय” के लिए लड़ने वालों ने लड़ाई जीतने के बाद यहां क्या किया। अरब के विभाजन के संबंध में 1915 और 1916 में जो गुप्त समझौते हुए थे उनका हाल लिका जा चुका है। उन समझौतों के अनुसार, युद्ध के दौरान ही इराक़, सीरिया और फ़िलिस्तीन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच विभाजित हो गए थे। लेकिन युद्ध के अंत तक, अरबों को आश्वस्त किया जाता रहा कि यह युद्ध केवल उन्हें तुर्कों के उत्पीड़न से छुटकारा दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है।
युद्ध के अंत में, फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा एक संयुक्त घोषणापत्र अरब देशों में प्रकाशित किया गया, जिसमें यह दावा किया गया था कि:
“यह युद्ध जो जर्मनी की विस्तारवादी दुस्साहसों से दुनिया को बचाने के लिए छेड़ा गया था, इसे पूर्व तक फैलाने का कारण केवल यह था कि ब्रिटेन और फ्रांस उन सभी राष्ट्रों को, जो लंबे समय से तुर्कों के अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार बने हुए थे, पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे और उनका उद्देश्य ऐसी राष्ट्रीय सरकारों और संस्थाओं की स्थापना करना था जो उन राष्ट्रों की इच्छाओं पर आधारित हों और जिनमें किसी अन्य का हस्तक्षेप न हो।”
लेकिन इन मौखिक घोषणाओं के साथ, जब अरबों ने मित्र राष्ट्रों की यह कार्रवाई देखी, कि सीरिया के तटों पर फ्रांसीसी सैनिक लगाए जा रहे थे और इराक़ और फ़िलिस्तीन में ब्रिटेन निरंकुश था, तो उन्हें पता चल गया कि उनके साथ धोखा किया गया है और यह चाल तुर्कों और अरबों में फूट डाल कर उनके देश छीनने के लिए चली गई थी। फिर उन्होंने इराक़, सीरिया और फ़िलिस्तीन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया और अमीर फैसल बिन हुसैन के नेतृत्व में सीरिया में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की।
उसी बीच, स्वयं मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध की लूट के वितरण को लेकर झगड़े शुरू हो गए। साइक्स-पिकोट संधि के अनुसार, मोसुल क्षेत्र फ्रांसीसी प्रभाव में दिया गया था, लेकिन वहाँ तेल के कुओं की बहुतायत को देखकर, ब्रिटेन का स्वार्थ उभर आया और उसने ख़ुद उस पर क़ब्ज़ा कर लिया। इसी तरह, यह निर्णय लिया गया कि फ़िलिस्तीन एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र बना रहेगा और केवल हाइफा पर ब्रिटेन का शासन होगा, लेकिन मिस्र के विद्रोह ने ब्रिटेन को मजबूर कर दिया कि वह स्वेज नहर के दूसरी ओर भी अपनी ताक़त बढ़ाए। अगर संभव हो तो, हाइफा से बसरा तक अपने लिए दूसरा रास्ता बनाए। अत: उसने फ़िलिस्तीन पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का निर्णय कर लिया। दूसरी ओर, सीरिया पर फ्रांसीसी प्रभाव भी ब्रिटेन को खटकता था और उसने अपने हित के लिए यह बेहतर समझा कि वहां उसके प्रभाव में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। इन मुद्दों पर लगभग डेढ़ वर्षों तक दोनों मित्रों के बीच विवाद चलता रहा और लूट के वितरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। लेकिन जब दोनों राज्यों ने इस आपसी संघर्ष का परिणाम यह देखा कि अरब राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हो रहा है, तो वे अपने संयुक्त हितों के लिए अरबों के ख़िलाफ़ एकजुट हो गए और अप्रैल 1920 में, उन्होंने तय कर लिया कि इराक़ और फ़िलिस्तीन ब्रिटिश क़ब्ज़े में रहेंगे और सीरिया पूरी तरह फ्रांस के क़ब्ज़े में रहेगा। यह बँटवारा उस बँटवारे से बिल्कुल भी अलग नहीं था जो लुटेरे किसी घर को लूटने के बाद करते हैं। उसके बाद, जनरल गॉर्ड ने एक लाख की सेना लेकर सीरिया की राष्ट्रीय सरकार पर हमला कर दिया और उन्हीं अरबों को बलपूर्वक प्राधीनता पर मजबूर किया गया, जिन्हें चार साल पहले दोस्त बनाया गया था और जिनकी मदद से तुर्कों को हराकर देश जीत लिया गया था। जिन्हें दो साल पहले तक आश्वासन दिया गया था कि हम केवल तुमको आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, जिन से युद्ध के बाद तक यह वादा किया जाता रहा था कि तुम्हारे देश पर तुम्हारा ही शासन होगा।
दूसरी ओर, ब्रिटिश उपनिवेश की घोषणा सुनकर क्रोधित हुए इराक़ के लोगों का बलपूर्वक दमन किया गया। “अत्याचारी” तुर्कों ने जहां कभी भी 14 हज़ार से अधिक सैनिकों को नहीं रखा था, “मुक्तिदाता” ब्रिटेन ने 90,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए। “अत्याचारी” तुर्कों ने जहां कभी साल में 200 अरबों की भी हत्या नहीं की थी, ब्रिटेन ने एक ही गर्मी (1920) में वहां दस हज़ार अरबों को मार डाला। और यह सब तब किया गया जब युद्ध में उन्हीं अरबों से यह कहकर मदद ली गई, “हम आपके दुश्मन नहीं, आपको आज़ादी दिलाने आए हैं।” अपने वादों की पवित्रता, और दूसरी ओर, ब्रिटिश जनता को संतुष्ट करने के लिए, जो इराक़ में एक वर्ष में दस लाख पाउंड की फिजूलखर्ची से बहुत नाराज थी, उसने इराक़ पर सीधे शासन करने के बजाय, एक कथित राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, जो जनरल मौड की घोषणा के विपरीत, इराक़ के लोगों की इच्छा के अधीन नहीं, बल्कि ब्रिटेन की इच्छा के अधीन रहे। इस उद्देश्य के लिए 1920 के वसंत में यह घोषणा की गई कि इराक़ के लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है, लेकिन इस घोषणा का पालन इस तरह किया गया कि इराक़ के लोगों को चुनाव का कोई अधिकार नहीं दिया गया। उनकी इच्छा के विरुद्ध, सीरिया के सिंहासन से वंचित हुए और दूसरे सिंहासन के इच्छुक फैसल बिन हुसैन को इस शर्त पर इराक़ के सिंहासन के लिए नामांकित किया गया था कि वह ब्रिटिश प्रभाव के तहत काम करेगा।इराक़ी जनता फैसल को बादशाह बनाने पर किसी तरह सहमत नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन ने उनकी आवाज़ को दबा दिया। प्रभावशाली इराक़ी नेता तालिब पाशा (जिन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटेन की बड़ी सेवा की थी) को गिरफ़्तार कर लिया गया और लंका में क़ैद कर लिया गया। और इराक़ के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए 23 अगस्त, 1922 को ऐसी हालत में शाह फैसल की गद्दी पर बैठने की घोषणा की गई, जबकि वास्तव में गद्दी तैयार भी नहीं हुई थी और शराब के पीपे रखकर एक अस्थाई गद्दी बना दी गई थी।
इस प्रकार फैसल को इराक़ का राजा बनाकर ब्रिटेन ने सिंहासन की क़ीमत मांगी। यह वही ब्रिटेन था, जो इराकियों को बचाने के लिए वहां गया था। वह क़ीमत क्या थी? बस इतनी थी कि इराक़ को एक ऐसे समझौते में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था जो अप्रत्यक्ष रूप से उसे पूर्णतः ब्रिटिश प्रभाव में ले जाता था। और इसके भाग्य का फ़ैसला हमेशा के लिए ब्रिटेन के हाथों में दे देता था। इस समझौते को इराक़ के लोगों ने एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए, इराक़ी लोगों की सहमति दर्ज करने का एक अनोखा तरीक़ा अपनाया गया था। उसे इराक़ी नेशनल असेंबली में आधी रात को पेश किया गया था। सदस्यों को पुलिस द्वारा उनके बिस्तरों से बलपूर्वक उठा लाया गया और ज़बरदस्ती उनसे वोट लेकर यह घोषणा कर दी गई कि इराक़ी संसद ने समझौते की पुष्टि कर दी है।
अब रहा तुर्की का दूसरा विभाजन, जिसे लेकर रूस के साथ 1915 में एक समझौता हुआ था। उसे बोल्शेविक क्रांति के कारण रद्द कर दिया गया और एक अन्य योजना बनाई गई जिसमें रूस के स्थान पर ग्रीस को तुर्की का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस योजना के अनुसार, यूनानियों ने पूर्वी थार पर क़ब्ज़ा कर लिया और स्मिर्ना (इज़ मीर) पर हमला किया और तुर्कों को उनकी मूल मातृभूमि के एक बड़े हिस्से से वंचित कर दिया। उसी समय, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और यूनानी सेनाओं ने कांस्टेंटिनोपल के विशेष शहर पर क़ब्ज़ा कर लिया और तुर्क से डेनियल पास और बोस्फोरस के दर्रे छीन लिए जो पहले रूस को देने का वादा किया गया था। इस दूसरे विभाजन को बाद में लॉज़ेन सम्मेलन में रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसे रद्द करने में न्याय की भावना का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि वास्तव में वह तुर्की तलवार थी, जिसने ग्रीस और मित्र राष्ट्रों को तुर्की छोड़ने पर मजबूर किया था।
युद्ध के “वैध” उद्देश्य
यही उन राष्ट्रों की सामरिक कार्यों का वृत्तांत है जो पश्चिमी सभ्यता के झंडावाहक हैं, बल्कि वास्तव में जिनकी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। यूरोप के कुछ प्रबुद्ध दार्शनिकों और विद्वानों को छोड़कर, जिनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जनता अपने-अपने शासकों की समर्थक थी और उसका उत्साहपूर्ण सहयोग उन शासकों के साथ था, जिसके बल पर वे इतना बड़ा युद्ध लड़ने में सक्षम हुए। इसलिए, उनकी बातचीत और तरीक़ों को देखकर, हम यह निष्कर्ष निकालने में सही हैं कि युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद “सत्य” और “न्याय” के नाम पर जो काम किए गए, वे ही वास्तव में पश्चिमी सभ्यता में “सत्य” और “न्याय” के उदाहरण हैं और पश्चिमी सभ्यता ऐसे “अधिकारों” के लिए तलवार उठाने की अनुमति देती है।
इस मानक के अनुसार पश्चिमी सभ्यता में युद्ध के जिन उद्देश्यों को जायज़ रखा गया है, वे इस प्रकार हैं:
* अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के धन का एकाधिकार प्राप्त करना
* अगर कोई प्रतिद्वंद्वी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उसका सिर कुचल देना।
* उन देशों को अपने अधीन लाना, जो दूर-दराज़ के क़ब्ज़ों के रास्ते में रुकावट हैं।
* देशों और साम्राज्यों के टुकड़े करना और कमज़ोर राष्ट्रों को ग़ुलाम बनाना।
* अगर किसी राष्ट्र से दुश्मनी हो जाए तो, उसे नष्ट कर देना या कम से कम उसकी ताक़त को तोड़ देना।
इन उद्देश्यों, को जिन्हें अक्सर “पवित्र अधिकार” के रूप में वर्णित किया गया है, को किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का विवेक इनके औचित्य और अनौचित्य और पवित्रता और अपवित्रता का निर्णय कर सकता है।
हो सकता है कि कुछ लोग तर्क की इस पद्धति को अतिशयोक्ति पर आधारित मान लें, लेकिन स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों के सामूहिक आचरण को ही पश्चिमी सभ्यता कहा जा सकता है। यूरोपीय राष्ट्र अपने धर्म को अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं और उनके धर्म को भी राजनीति में शामिल होना पसंद नहीं। क़ानून को भी मानक माना जा सकता था, लेकिन वे क़ानून भी युद्ध के वैध और अवैध उद्देश्यों पर कोई चर्चा नहीं करते है। दोनों चीज़ो को अलग कर देने के बाद अब हम पश्चिमी सभ्यता की मान्यता किससे पूछें? क्या नैतिकता के विद्वानों से पूछें? क्या उन विचारकों से पूछते हैं जो शांति का उपदेश देते हैं? क्या उन गिने चुने लेखकों से पूछें जिनकी क़लम से कभी-कभी मानवता और मानव भाईचारे के दिल को छू लेने वाले विचार टपकते हैं? हमें इन लोगों से पूछने में कोई संकोच नहीं, लेकिन हमें उनमें से हज़ार दो हज़ार नहीं, केवल एक या दो ऐसे लोगों का नाम बता दिया जाएं, जिनके कथन पश्चिमी देशों के लिए प्रमाण का दर्जा रखते हों, और जिनके विचार को सभी नहीं तो पश्चिमी समुदाय के अधिकांश लोग मान्यता देते हों। अगर पश्चिम में किसी चीज़ पर ऐसी सर्वसम्मति नहीं है, तो हमारे पास पश्चिमी राष्ट्रों के आचरण और उनके सामान्य तरीक़ों के सिवा और क्या रह जाता है, जिससे हम युद्ध के संबंध में पश्चिमी देशों के नैतिक मूल्यों का पता लगा सकें ?
राष्ट्र संघ
महायुद्ध के बाद, विजयी पश्चिमी शक्तियों ने राष्ट्रपति विल्सन की सलाह पर लीग ऑफ नेशंस नामक एक संघ का गठन किया। इस संघ का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध और युद्ध के कारणों को समाप्त करना था। अतः युद्ध के कारणों का अंत करने के लिए, उसने एक अंतरराष्ट्रीय न्यायिक विभाग की स्थापना की ताकि वह राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाए। इस के लिए, राज्यों के बीच एक समझ बनाई गई, ताकि मैत्रीपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो सके, और अगर कोई राज्य अपने हित के लिए तलवार का उपयोग करे, तो सभी राज्य मिलकर उसको सीधे रास्ते पर लाएं। इस समझौते के अनुच्छेद 16 के शब्द हैं:
“अगर राष्ट्र संघ के किसी सदस्य ने इस समझौते के अनुच्छेद 12,13,15 का उल्लंघन करते हुए युद्ध शुरू करदी है, तो उसका यह कार्य राष्ट्र संघ के अन्य सभी सदस्यों के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा जैसा होगा। राष्ट्र संघ के सदस्य इस समझौते के माध्यम से शपथ लेते हैं कि वे समझौता तोड़ने वाले राज्य के साथ अपने वित्तीय और वाणिज्यिक संबंध समाप्त कर लेंगे और अपने नागरिकों का उसके नागरिकों के साथ लेन-देन भी रोक देंगे। इसके अलावा, वे उस राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों के नागरिकों के साथ व्यावसायिक वित्तीय या व्यक्तिगत संबंध रखने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वे राज्य संघ के सदस्य हों या न हों।”
उसके बाद, संघ को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपराधी राज्य को रास्ते पर लाने के लिए अपने सदस्यों से जितनी सेना और नौसैनिक बल उचित समझे, माँगे, और यह सभी सदस्यों का दायित्व ठहराया गया कि वे अपने वित्तीय और सामरिक संसाधनों को उस अपराधी राज्य के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए संघ को सौंप दें।
यह समझौता बाहर से तो युद्ध को रोकने का एक बहुत ही प्रभावी और अचूक हथियार प्रतीत होता था, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उसी गुटबंदी का एक अधिक सभ्य और अधिक ख़तरनाक रूप निकला, जिसके कारण 1914 में महायुद्ध हुआ था। चूंकि युद्ध के दौरान उस गुटबंदी के भयानक परिणामों को देखकर पूरा यूरोप उससे घृणा करने लगा था और उसे अपने सभी दुखों का कारण मानने लगा था, इसलिए पश्चिमी साम्राज्यों को उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसके बिना, उनके राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं थी। क्योंकि अकेले किसी भी राज्य का इतना प्रभाव नहीं हो सकता था कि वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सके और अपने लक्ष्य पा सके। सामान्य लक्ष्यों के लिए यह आवश्यक है कि बड़े बड़े राज्य एक संयुक्त बल के साथ दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने उसी गुटबंदी को एक दूसरा रूप दे दिया, जिसमें भीड़ की रक्षात्मक एकता के स्थान पर शांतिप्रियता और धर्मपरायणता की आड़ में वही आपराधिक एकता और सहयोग की भावना भरी हुई थी। यह गठबंधन छोटे राज्यों को दबाने में बहुत उपयोगी था। अगर ग्रीस और बुल्गारिया में विवाद होता, या पोलैंड और लिथुआनिया ने झगड़ा हो जाता, तो राष्ट्र संघ के बड़े सदस्य उन्हें एक ही धमकी में सुधार सकते थे। इससे बड़ा फ़ायदा यह था कि राष्ट्र संघ के नेताओं का आतंक और प्रभाव भी पूरी दुनिया पर क़ायम हो जाता और वे “आर्मी ऑफ गॉड” बन कर दुनिया पर राज करते। वे संसार की व्यवस्था में संशोधन करने, शक्तियों को कम करने या बढ़ाने, और अवांछित शक्तियों को डराने की सेवा दे सकते थे। लेकिन अगर कोई प्रमुख शक्ति स्वयं सामूहिक समझौते का उल्लंघन कर देती तो संघ उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना तो दूर, मौखिक पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। और अगर करती भी तो उसका कोई असर नहीं हो सकता।
निरस्त्रीकरण के आधुनिक प्रस्ताव
यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले वर्षों में निरस्त्रीकरण और युद्ध निषेध के मुद्दों पर विभिन्न प्रस्तावों पर गरमागरम बहस हुई हैं और कई आशावादी लोग उन्हें पश्चिमी देशों की सद्भावना का प्रमाण समझने लगे।लेकिन सच तो यह है कि इन सारी बातों में सच की परछाई भी नहीं है। चूँकि पश्चिम के आम लोग लड़ते-लड़ते थक चुके हैं, और उन्हें अपने सामूहिक और विशेष रूप से व्यावसायिक और औद्योगिक जीवन में आराम की सख़्त ज़रूरत है, इसलिए वे दिल बहलाने के लिए ऐसे सुझाव और कल्पनाएँ सुनना पसंद करते हैं, जिन से अगर शांति नहीं, तो ही शांति की भ्रमपूर्ण अपेक्षा ही स्थापित हो जाती है। वरना जहां तक कार्रवाई का सवाल है, तो इन अपेक्षाओं के पूरा करने का इसके पास कोई उपकरण नहीं है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों में युद्ध के संसाधन ने जो विकास हासिल किया है, वह पहले कभी नहीं हुआ। मौखिक रूप से तो ज़रूर ऐसी बातें कही जा रही हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि पश्चिम के लोग युद्ध और रक्तपात से तंग आ चुके हैं, शांति और सद्भाव के पक्षधर हैं और अपने ही लोगों के विनाश के खेल को रोकना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि इन राष्ट्रों के बीच घोर शत्रुता बढ़ रही है। उनके हृदय में ज्वालामुखी पक रहे हैं। उनकी सेनाएँ संख्या और शक्ति में बढ़ती जा रही हैं। उनके युद्ध के हथियार दिन-ब-दिन विकसित हो रहे हैं और हर देश आने वाले युद्ध में ख़ुद को अपने प्रतिद्वंद्वियों से अधिक शक्तिशाली साबित करने और सभी विरोधी ताक़तों का सफ़ाया कर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, कौन कह सकता है कि पश्चिमी देशों में शांतिवाद का वास्तविक संतुलन है और वे वास्तव में युद्ध से दूर हो गए हैं?
आज पश्चिमी सभ्यता ने बड़ी संख्या में सेनाएँ, युद्ध के घातक हथियार, विशाल युद्धपोत, विनाशकारी फाइटर जेट, जहरीली गैसों का भंडार और इतनी विनाशकारी युद्ध सामग्री इकट्ठा कर रखी है जिससे पूरी दुनिया को एक नहीं कई बार नष्ट किया जा सकता है। इन तथ्यों को देखकर भला कौन है, जो शांतिवाद की झूठी बातों और शांति स्थापना के दिखावे के सम्मेलनों से धोखा खा जाएगा?
युद्ध के व्यावहारिक पहलू
अब तक जो कुछ व्यक्त किया गया है उसका संबंध पश्चिमी युद्ध की नैतिक स्थिति से था। इस पहलू में आपने देखा कि जहां तक युद्ध के उद्देश्यों और लक्ष्यों का सवाल है, पश्चिमी दुनिया अपनी सभ्यता के सारे विकास के बावजूद उस बिंदु से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई है, जिस पर अंधकार युग के असभ्य और बर्बर राष्ट्र सदियों पहले स्थापित थे। युद्ध के संसाधनों में तो उन्होंने विकास के आसमान छु लिए, मगर इस युद्ध के भीतर जो भावना काम कर रही है वह उसी अंधकार और बर्बर युग की भावना है। प्राचीन काल के बर्बरों की तरह, इन आधुनिक बर्बरों के पास भी कोई ऊँचे आदर्श नहीं हैं, कोई ऊँची महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई नैतिक उद्देश्य नहीं है जिसके आधार पर इनकी श्रेष्ठता का दावा किया जा सके। धन-दौलत हासिल करने और सत्ता का विस्तार करने की वही इच्छा, जो आज से चार हज़ार साल पहले एक असभ्य जनजाति को युद्ध के लिए उकसा सकती थी, आज भी सभ्य राष्ट्रों को नरसंहार और रक्तपात के लिए प्रेरित करती है। सभ्यता के विकास से नैतिक स्थिति में कोई विकास नहीं हुआ। अगर कोई प्रगति हुई है, तो वह यह है कि पहले इन तुच्छ और अनैतिक उद्देश्यों के लिए जो बल प्रयोग किया जाता था, अब उससे दस हज़ार गुना अधिक गंभीर, भयानक और विनाशकारी बल प्रयोग किया जाता है।
ज़ाहिर है कि जब लक्ष्य प्रतिष्ठा और पवित्रता से रहित हो तो लक्ष्य प्राप्ति की विधि कितनी भी अच्छी और शुद्ध क्यों न हो, उससे कोई कर्म भलाई और पवित्रता के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी हमें यह देख लेना चाहिए कि पश्चिमी सभ्यता ने अपने युद्ध कार्यों को कैसे क़ानूनों से विनियमित किया है और इस्लामी क़ानूनों की तुलना में इन क़ानूनों की व्यावहारिक स्थिति क्या है। पश्चिम के लोगों का दावा है कि उन्होंने पुराने दिनों के बर्बर तरीक़ों को छोड़कर युद्ध के अधिक सभ्य तरीक़ों को अपना लिया है। वह युद्ध, जो जानवरों के खेल से बहुत अलग नहीं था, एक सभ्य झड़प और एक महान संघर्ष में बदल गया है। यह दावा इतनी भव्यता के साथ और इतनी धूमधाम से किया जाता है कि बिन दुनिया इसे सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास कर लेती है। लेकिन हम इसे कसौटी पर परख कर देखना चाहते हैं यह वास्तव में कहां तक सच है?
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की वास्तविकता
पश्चिमी देशों के आपस के मामलों, शांति और युद्ध के संबंधों को नियंत्रित करने वाले क़ानून को अंतर्राष्ट्रीय क़ानून कहा जाता है। क़ानूनी विद्वानों ने इसे अलग-अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे व्यापक परिभाषा यह है:
“यह एक प्रचलन है, जिसका पालन सभ्य राष्ट्र अपने मामलों में करते हैं।”
यह प्रचलन किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जिसका पालन करने के लिए ये देश मजबूर हों, और इन देशों के पास इसे बदलने का अधिकार न हो। बल्कि, उन्होंने स्वयं अपनी सुविधा के लिए इसे तैयार किया है, और इस आधार पर उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है कि अपने उद्देश्यों के अनुसार इसे जैसे चाहें बदल लें, और जब चाहें इसे छोड़ कर दूसरा तैयार कर लें। इसलिए यह कहना अधिक सही है कि पश्चिमी देश अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून उनका अनुयायी है। अपनी सुविधा के लिए वे जो तरीक़ा अपनाते हैं, वही क़ानून है और जिस तरीक़े को वे छोड़ देते हैं, वह क़ानून नहीं है। आज, पश्चिमी दुनिया जिन सिद्धांतों का पालन करने के लिए सहमत है, वे आज के अंतर्राष्ट्रीय क़ानून हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि यही कल का क़ानून भी हो। कल अगर वे इन नियमों में परिवर्तन करके कुछ और नियम बना लेते हैं तो यह क़ानून रद्द हो जायेगा और वे नये नियम अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून बन जाएंगे।
यही कारण है कि पश्चिम के कुछ प्रमुख विद्वानों की राय में इस प्रचलन को ‘क़ानून’ शब्द से व्यक्त करना ग़लत है। ऑस्टिन अपनी किताब “प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमाइंड” में लिखते हैं:
“अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का बल केवल जनमत के समर्थन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे सही अर्थों में क़ानून नहीं कहा जा सकता है।”
लॉर्ड सैलिसबरी कहते हैं:
“इसे किसी भी अदालत द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे ‘क़ानून’ शब्द से व्यक्त करना भ्रामक है।”
1871 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का फ़ैसला करते हुए यह व्याख्या की थी कि:
“समुद्र का क़ानून, भी सभी अंतरराष्ट्रीय क़ानून की तरह, सभ्य राष्ट्रों की सामूहिक सहमति पर टिका हुआ है। यह अगर लागू है, तो, इसलिए नहीं कि किसी श्रेष्ठ शक्ति ने इसे अधिनियमित किया है, बल्कि केवल इसलिए कि यह आम तौर पर एक प्रचलन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।”
लॉर्ड बरकिंडा ने अपनी किताब, इंटरनेशनल लॉ में कहा है कि इस क़ानून का अस्तित्व और स्थिरता केवल तीन चीज़ों पर निर्भर करती है:
1 राष्ट्रीय सम्मान की भावना जो अंतरराष्ट्रीय जनमत के प्रभाव से पैदा होती है (हालांकि यह अक्सर समय की ज़रूरतों के प्रभाव में मर भी जाती है)।
2. सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्यों के सिवा मामूली उद्देश्यों के लिए युद्ध के नुक़सान को सहन करने की अनिच्छा।
3. राष्ट्र महसूस करते हैं कि ये निश्चित क़ानून उनकी अपनी सुविधा के लिए हैं और उनका अस्तित्व इन क़ानूनों के प्रति उनकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है।
एक अन्य स्थान पर बिरकिंड लिखते हैं:
“सैद्धांतिक रूप से, जनता की राय और संबंधित सरकार की स्वैच्छिक प्रस्तुति के अलावा अंतरराष्ट्रीय क़ानून के प्रावधानों के पीछे कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
इन कहावतों से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय क़ानून केवल कुछ देशों का प्रचलन है जिसका कोई क़ानूनी मूल्य नहीं है और न ही कोई स्थिर आधार है।
अंतर्राष्ट्रीय क़ानून का सामरिक विभाग
लेकिन इस क़ानून का वह हिस्सा जिसे युद्ध का क़ानून कहा जाता है, शांति के क़ानून से भी कमज़ोर है। पश्चिम में युद्ध का क़ानून वास्तव में किसी नैतिक आधार पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल इस तथ्य पर आधारित है कि राज्य स्वयं अपने लोगों को क्रूरता और भयानक पीड़ा से बचाना चाहते हैं। इसी लिए उन्होंने मिलकर यह निश्चय कर लिया है कि जब भी हम आपस में लड़ेंगे तो उक्त नियमों का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, 1907 के हेग सम्मेलन में, उन्होंने एक संधि की, जिसमें युद्ध के क़ैदियों के लिए कई रियायतें और सुविधा की चीज़ें निर्धारित की गईं। ऐसा नहीं है कि वे उन लोगों के प्रति दयालु होना अपना नैतिक दायित्व समझते थे जो उनसे लड़ने आएं, बल्कि उसका असली कारण बस इतना ही था प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के सैनिकों को सुरक्षित रखना चाहता था और चाहता था कि जब उन्हें दुश्मन द्वारा गिरफ़्तार कर लिया जाए तो बदले की भावना से उनपर अत्याचार न किया जाए। अगर कोई राज्य आज इस समझौते को तोड़ता है और युद्ध बंदियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसा कि रोम और ईरान के साम्राज्यों ने 6वीं शताब्दी में किया था, तो शायद सभ्य से सभ्य राज्य भी संधियों को ताक़ पर रखकर उस से भी बढ़कर क्रूर तरीक़ा अपनाने में एक क्षण की भी देरी लगाने में संकोच नहीं करेगा। यही हाल उन क़ानूनों का भी है, जो विमानों की गोलाबारी, विस्फोटक गोले और जहरीली गैसों के उपयोग, युद्ध अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं, और इसी तरह के अन्य युद्ध मामलों से जुड़े हैं। उनके बारे में जितने समझौते हैं, उन सभी का कारण यह है कि प्रत्येक राज्य अपनी सेनाओं और नागरिक आबादी को विनाश और मृत्यु से बचाना चाहता है, अन्यथा किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, कोई भी राज्य उन नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है।
अतः ये नियम और क़ानून, जिन्हें युद्ध के “सभ्य” क़ानून कहा जाता है, वास्तव में क़ानून नहीं बल्कि संधियाँ हैं। ये तभी लागू हो सकते हैं जब सभी अनुबंधित शक्तियाँ उन्हें स्वीकार कर लें। कोई राज्य केवल उसी समय तक उस के पालन को बाध्य रह सकता है, जब तक अन्य राज्य भी उसका पालन करते रहें। जैसे ही एक बड़े राज्य या कुछ राज्यों के संग्रह ने उनका उल्लंघन किया, दुनिया के सभी सभ्य राज्य उसके पालन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे नियमों को किसी भी तरह से “क़ानून” नहीं कहा जा सकता है। क़ानून की परिभाषा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति/पक्ष उसका पालन करने के लिए बाध्य हो, चाहे दूसरे इसका पालन करें या न करें। जिस नियम का पालन दूसरे पक्षों द्वारा उसके पालन पर निर्भर हो, वह क़ानून नहीं, बल्कि अनुबंध है। अनुबंध, चाहे उसमें नियम और क़ानून कितने ही अच्छे क्यों न हों, किसी प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि इसके नियम-कायदे अनुबंधिंयों के स्वार्थ पर आधारित होते हैं, न कि नैतिक दायित्व की भावना पर।
यह केवल हमारा मत नहीं है, यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता भी यही कहते हैं। सर थॉमस बार्कले अपने एक निबंध के अंत में लिखते हैं:
युद्ध के संचालन को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। युद्ध की अत्यावश्यकताएं, आवेग और अतिउत्साह, जो युद्ध की स्थिति में हमेशा प्रबल होते हैं, उन सर्वोत्तम नियमों को भी तोड़ डालते हैं, जिन्हें कूटनीति अपनी अत्यधिक बुद्धिमत्ता के साथ निर्धारित करती है। हालाँकि, ये नियम जनमत की स्थिति को दर्शाते हैं, जो सभ्य राष्ट्रों में बर्बर कृत्यों की रोकथाम करती है।”
इस के बाद इन क़ानूनों में जो कुछ जान बची रह जाती है उसे युद्ध की आवश्यकताओं का प्रभावशाली क़ानून और भी कमज़ोर कर देता है। युद्ध के मैदान की ज़रूरतें हमेशा इन क़ानूनों से टकराती हैं और किताबों में लिखे और शांति सम्मेलनों द्वारा बनाए गए क़ानून हमेशा पराजित होते हैं। प्रोफेसर नेपोल्ड लिखते हैं:
“अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के अन्य क्षेत्रों की तुलना में युद्ध के क़ानून के नियमों में विरोधाभास और असहमति बहुत अधिक होती है, क्योंकि युद्ध के क़ानून और युद्ध की ज़रूरतों में संघर्ष होता रहता है। इसलिए, युद्ध के क़ानून को अंतरराष्ट्रीय क़ानून में शामिल करने का नतीजा यही हो सकता है कि जो अस्थिरता युद्ध के क़ानून की है वही वही दूसरे अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की भी हो जाए।”
जिस समय हेग में युद्ध के नियम तैयार किए जा रहे थे, यूरोप के राजनीतिज्ञों पर दिखावे की सभ्यता इतनी हावी थी कि उन्होंने अपने लोगों की वास्तविक युद्ध प्रवृत्तियों और झुकावों और उनकी युद्ध सम्बंधी आदतों को नज़रअंदाज़ करके कुछ ऐसे क़ानून बना लिए जो देखने में बहुत ही सभ्य, बहुत शानदार और अत्यधिक मानवतावादी थे, लेकिन वास्तव में उनके सैन्य समूह उनका पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जर्मन सैन्य प्रतिनिधि मार्शल बी. बर्स्टीन ने सम्मेलन की शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी कि:
“हम जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून बनाना चाहते हैं, उसमें केवल वे ही प्रावधान होने चाहिए जिनका पालन युद्ध की दृष्टि से विशिष्ट परिस्थितियों में भी किया जा सके।”
यह स्पष्ट है कि वास्तविक विश्वसनीयता कथन नहीं बल्कि व्यवहार की है। कहने वाला कुछ भी कहे, हमें तो यह देखना होगा कि करने वाला क्या करता है। हमारी दृष्टि में, पश्चिम में युद्ध का वास्तविक नियम वह नहीं है जो कागजों में लिखा है, बल्कि वह है जिसका पश्चिम के लोग युद्ध में अभ्यास करते हैं। इसलिए, हम क़ानूनी समूह को नहीं बल्कि सैन्य समूह को विश्वसनीय समझते हैं। युद्ध के नियमों के बारे में इस समूह के विचारों का अध्ययन करने से पश्चिम के लोगों का वास्तविक झुकाव देखा जा सकता है।
यूरोप के प्रसिद्ध रणनीतिकार क्लॉज विट्स अपनी किताब (योम क्रीज) में लिखते हैं:
“युद्ध के नियम अपने आप लगाए गए प्रतिबंध हैं। ये समझ में आने वाले नहीं हैं और इनका उल्लेख भी कठिन है।जिन्हें “युद्ध के प्रचलन” कहा जाता है। अब मानवता प्रेमियों के लिए अपने विचार में यह समझ लेना बहुत आसान है कि दुश्मन को बड़े रक्तपात के बिना निहत्था पराजित कर लेने का एक समझदारी भरा तरीक़ा मौजूद है, और यह युद्ध कला का उचित लक्ष्य है।
लेकिन यह विचार, चाहे कितना भी सुखद और लुभावना लगे, वास्तव में पूरी तरह से ग़लत है और इसे जितनी जल्दी दूर कर दिया जाए, इतना ही बेहतर है। युद्ध जैसी भयानक चीज़ में दया और उपकार की भावना को डालने से जो बुराइयाँ पैदा होती हैं, वे और भी बुरी हैं। युद्ध के दर्शन ही में नर्मी और संयम के सिद्धांत को प्रवेश देना एक ग़लती है। युद्ध अनिवार्य रूप से जब्र और ज़बरदस्ती का कार्य है जो किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं कर सकता है।
जहां तक सिद्धांतों का संबंध है, हमने पश्चिमी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय क़ानून और उसके युद्ध विभाग की वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया है। यह क़ानून क्या है? क़ानून के रूप में इसका मूल्य क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से इसका क्या प्रभाव है? फिर उनकी अपनी नज़र में उनके युद्ध विभाग की क्या हैसियत है? उस में युद्ध को नैतिक मर्यादाओं में बाँधने की शक्ति कहाँ तक है? व्यवहारिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से युद्ध को नियन्त्रण और व्यवस्था में लाने में वह किस हद तक प्रभावी हो सकता है? उपरोक्त संक्षिप्त चर्चा से ये प्रश्न कुछ हद तक स्पष्ट हो गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम में जिसे युद्ध का क़ानून कहा जाता है, वास्तव में वह क़ानून है ही नहीं।
अब हम यह देखना चाहते हैं कि यह तथाकथित क़ानून युद्ध को सीमित करने और संगठित करने में कहाँ तक सफल रहा है? इसने जो सीमाएँ और नियम निर्धारित किए हैं, वे इस्लामी क़ानून द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में कैसे हैं? इसके दिखावटी और वास्तविक नियमों में क्या अंतर है? वास्तव में इसने मानवता की कितनी सेवा की है?
युद्ध की घोषणा
युद्ध के मुद्दों में पहला मुद्दा यह है कि युद्ध की शुरुआत कैसे की जाए। पुराने समय में यह प्रचलन था कि युद्ध शुरू करने से पहले दूतों के माध्यम से दुश्मन को सूचित कर दिया जाता था। उस युग में अंतरराष्ट्रीय क़ानून के लेखकों ने भी घोषणा और चेतावनी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, उनमें से कुछ का मत था कि बिना घोषणा के आक्रमण करना सही नहीं है। लेकिन बाद में, क़ानूनी विशेषज्ञों का झुकाव इस ओर हो गया कि युद्ध की औपचारिक घोषणा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए, राज्यों ने आम तौर पर यह नियम अपना लिया कि वे युद्ध की घोषणा किए बिना ही कार्रवाई शुरू कर देते थे। इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 1700 से 1872 तक यूरोप में 120 युद्ध हुए, जिनमें से केवल दस युद्धों की आधिकारिक घोषणा की गई। इनमें से कुछ लड़ाइयाँ ऐसी थीं जो राजनयिक संबंधों के टूटने से पहले ही छेड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए, 1812 में, संबंधों के टूटने से पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बंदरगाह में मौजूद सभी अंग्रेज़ी जहाज़ों को ज़ब्त कर लिया और बिना सूचना के कनाडा पर हमला कर दिया। इसी तरह, 1854 में, ब्रिटेन ने काला सागर में रूसी बेड़े पर हमला किया और इसे सियास्टॉप्स तक भगा दिया, हालाँकि उस समय तक दोनों पक्षों के राजदूत वापस नहीं आए थे। फिर, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, यूरोप फिर से पहले तरीक़े की ओर लौट आया, और युद्ध से पहले युद्ध की घोषणा की जाने लगी। इस प्रकार, जर्मनी और फ्रांस के बीच 1870 का युद्ध, तुर्की और रूस के बीच 1877 का युद्ध, अमेरिका और स्पेन के बीच 1898 के युद्धों की शुरुआत औपचारिक घोषणा से हुई। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में बिना किसी घोषणा के रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया और जापान ने अचानक रूस पर हमला कर दिया।
20वीं शताब्दी के आरंभ तक, युद्ध की शुरुआत करने के बारे में कोई नियम नहीं था। राज्य जब चाहते थे तब अचानक शत्रु पर आक्रमण कर देते थे और जब उचित समझते थे तो युद्ध की घोषणा भी पहले ही कर देते थे। 1907 के हेग सम्मेलन में पहली बार इस संबंध में एक नियम बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए एक समझौता किया गया, जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं:
पहली धारा : राज्य यह वचन देते हैं कि उनके बीच युद्ध तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि पहले से स्पष्ट चेतावनी नहीं दी जाती है। यह चेतावनी युद्ध की घोषणा के रूप में हो सकती है जिसमें युद्ध के कारण बताए गए हों या अल्टीमेटम के रूप में जिसमें युद्ध की सशर्त घोषणा की गई हो।
दूसरी धारा : तटस्थ शक्तियों को युद्ध की स्थिति के अस्तित्व के बारे में बिना किसी देरी के सूचित किया जाना चाहिए, और जब तक अधिसूचना की प्राप्ति न हो जाए (जो हमेशा तार द्वारा होनी चाहिए) तब तक, तटस्थों के बारे में युद्ध के क़ानून लागू न हों।
यूरोप में यह सभ्य क़ानून 20वीं शताब्दी में आकर अधिनियमित किया गया है, और वह भी केवल समझौते के प्रतिभागियों के लिए। लेकिन इस्लाम में कोई चौदह सौ साल से यह क़ानून मौजूद है कि जिस क़ौम के साथ तुम्हारी सन्धि हो उस के ख़िलाफ तब तक युद्ध न करो, जब तक उसे सूचित न कर दो कि अब तुमिहारी उक्त गलतियों के कारण तुम्हारे और हमारे बीच सन्धि बाक़ी नहीं रही। अब हम और तुम दुश्मन हैं। यह क़ानून इस शर्त के अधीन नहीं है कि यह केवल उन राष्ट्रों के मामले में अपनाया जाएगा जिन्होंने हमसे वादा किया है कि वे भी हमारे ख़िलाफ़ कभी अचानक युद्ध नहीं छेरेंगे।
लड़ाके और ग़ैर-लड़ाके
दो राष्ट्रों के बीच युद्ध की स्थिति स्थापित हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि युद्धरत राष्ट्र के सदस्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? सत्रहवीं शताब्दी तक, यूरोप युद्धरत्त (Belligerent) और योद्धा (Combatant) के बीच के अंतर से अपरिचित था। उनके अनुसार, प्रत्येक युद्धरत्त एक योद्धा था, इसलिए उसे मारना और उसकी संपत्ति हड़प करना जायज़ था, चाहे वह महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो या कोई और। बाद में सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में अंतरराष्ट्रीय क़ानून के लेखकों ने वर्ग के आधार पर लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच अंतर करने की कोशिश की, लेकिन कोई व्यापक विभाजन पर सहमति नहीं बन सकी। 19वीं शताब्दी में, इस प्रश्न का समाधान कर दिया गया क्योंकि जो युद्ध अभियानों में भाग लेते हैं वे लड़ाके होते हैं और जो उनमें भाग नहीं लेते वे ग़ैर-लड़ाके होते हैं। लेकिन यह समाधान बहुत ही जटिल था। उसके बाद, फिर यह नियम निर्धारित किया गया कि केवल दुश्मन की नियमित सेना को योद्धा या लड़ाकों में गिना जाएगा और अन्य सभी वर्गों को ग़ैर-लड़ाकों में शामिल किया जाएगा। लेकिन इससे कुछ और जटिल मुद्दे उठ खड़े हुए। स्वाभाविक रूप से यह सवाल पैदा होता है कि अगर किसी देश के निवासी अपने देश के बचाव में हथियार लेकर खड़े हो जाएं और बिना किसी अनुशासन के दुश्मन के साथ युद्ध शुरू कर दें, तो उनकी स्थिति क्या होगी? क्या उन्हें लड़ाकों के रूप में गिना जाएगा और उन्हें दुश्मन की नियमित सेना के समान अधिकार दिए जाएंगे? या उन्हें ग़ैर-लड़ाकों में शामिल कर के युद्ध के नियम के अनुसार लुटेरों में गिना जाएगा? ऊपर वर्णित क़ानून कहता है कि अगर वे युद्ध की कार्रवाई में भाग लेते हैं, तो उन्हें न लड़ाकों की सुविघा मिलेगी न ग़ैर-लड़ाकों की छूट। अर्थात अगर वे क़ैद होंगे तो मार दिये जाएंगे, और अगर घायल होंगे, तो इलाज और उपचार से वंचित रहेंगे। लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच भेद का सिद्धांत, जो इस क़ानून द्वारा स्थापित किया गया था, उन राष्ट्रों के लिए असाधारण विनाश और पीड़ा का कारण बन गया, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर लड़ते हैं और किसी भी नियमित युद्ध प्रणाली में शामिल नहीं होते हैं।
1870 के युद्ध में, जब फ़्रांस ने अपनी सामान्य आबादी को सेना में भर्ती करना शुरू किया और जर्मनी ने उन्हें लड़ाकों के अधिकार देने से इनकार कर दिया, तो यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के सामने अपने पूरे महत्व के साथ आ गया। 1874. ब्रसेल्स सम्मेलन में इस पर बड़ी बहस हुई. अंत में, लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच एक निश्चित अंतर स्थापित किया गया, जिसके अनुसार केवल उन्हीं लोगों को लड़ाका माना गया, जो:
1. एक ऐसे नेता के अधीन रहें जो अपने अधीनस्थों के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार हो।
2. अपने शरीर पर ऐसे निश्चित चिह्न लगाएं जो दूर से ही पहचाने जा सकें।
3. खुल्लम खुल्ला हथियार उठाएं।
4. युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन करें!
1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों में इसी अंतर को मान्यता दे दी गई।
इस प्रकार एक प्रश्न तो अवश्य हल हो गया, किन्तु दूसरा प्रश्न शेष रह गया, शस्त्र उठाने की ज़रूरत केवल मुक्त राष्ट्रों को ही नहीं होती है, अपितु कभी-कभी अर्ध-मुक्त और दास राष्ट्रों को भी अपने हड़पे हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हथियार उठाना पड़ता है। स्वतंत्रता के लिए लड़ना प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है, या अगर वह किसी शक्तिशाली शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तलवार का सहारा लेता है, तो उसे किसी भी तर्क से अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई देश ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए लड़ता है, तो क्या उसके सभी लोग अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे? क्या वे दस्युओं और लुटेरों की तरह पकड़े और मारे जाएँगे?
इन सवालों को हेग ट्रिब्यूनल द्वारा हल करने की कोशिश नहीं की गई है, और वास्तव में पश्चिमी देशों का झुकाव यह है कि ऐसे राष्ट्र न तो लड़ाकों के अधिकारों का आनंद ले सकते हैं और न ही ग़ैर-लड़ाकों की रियायतें। उनके भाग्य में लिखा है कि उन्हें तोपों और बंदूकों का निशाना बना दिया जाए। उनकी आबादियों का जनसंहार किया जाए और उनके लोगों को पकड़कर मार डाला जाए। हमारी आंखों के सामने भारत में ब्रिटेन द्वारा, रीफ में स्पेन द्वारा, और सीरिया में फ्रांस द्वारा किए गए भयानक अत्याचार इस बात का प्रमाण हैं कि पश्चिमी सभ्यता का क़ानून किसी भी राष्ट्र के इस अधिकार को मान्यता नहीं देता है कि वह आज़ादी हासिल करने के लिए युद्ध करे।
लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच अंतर का यह नियम इस अर्थ में भी ग़लत है कि यह युद्ध में हथियार नहीं उठाने वाले सभी लोगों को ग़ैर-लड़ाकों के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि युद्ध में सभी ग़ैर-सैनिक वर्गों को ग़ैर-लड़ाका टहराना, उन्हें लड़ाई से सुरक्षित रखकर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने देना और उन्हें वे सभी सुविधाएं देना, जो ग़ैर-लड़ाकों के लिए आरक्षित हैं, न केवल व्यवहार में असंभव है बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी ग़लत है।
इस अर्थ में, पश्चिमी क़ानून द्वारा लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच खींची गई अंतर की रेखा किसी भी तरह से सीधी नहीं है। एक ओर, यह उन कई वर्गों को लड़ाकों के अधिकारों से वंचित कर देती है जो वास्तव में इसके हक़दार हैं। दूसरी ओर, बहुत से ऐसे वर्गों को ग़ैर-लड़ाकों की रियायतें दे देती है, जो उसके पात्र नहीं हैं।
लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच इस्लाम ने इन दोनों अतियों से दूर एक सीधी रेखा खींची है, जो लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों को उनके पेशे के आधार पर विभाजित नहीं करती है, बल्कि उन्हें लड़ने की क्षमता के आधार पर विभाजित करती है। इसने युद्धरत राष्ट्र को इस आधार पर विभाजित किया है कि जो लोग स्वभाव और आदत से लड़ते हैं या लड़ने में सक्षम हैं, वे सभी लड़ाका हैं, और जिनमें स्वभाव और आदत से लड़ने की क्षमता नहीं है, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, विकलांग, आदि, वे सभी ग़ैर-लड़ाके हैं। दुश्मन राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति जो मुसलमानों से लड़ने के लिए आता है, चाहे वह नियमित सेना से संबंधित हो या नहीं, उसे एक लड़ाका माना जाएगा और उसे सेनानियों के लिए आरक्षित सभी अधिकार दिए जाएंगे, बशर्ते कि वह वचन भंग और विश्वासघात का अपराधी न हो । इसी प्रकार युद्ध में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति की गणना योद्धा में की जाएगी और उसे युद्ध की ज़रूरतों के अधीन न कि अनिवार्य रूप से युद्ध में भाग लेना होगा। यह निश्चित है कि अगर वह शांति मांगेगा, तो उसे शांति मिलेगी। अगर वह दारुल-हर्ब (जिस राज्य से युद्ध हो रहो हो) और दारुल-इस्लाम के बीच शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहता है, तो युद्ध के अपवाद के साथ इसकी भी अनुमति दी जा सकती है। अगर वे युद्ध से दूर रहकर अपने व्यापार में लगें तो अयोद्धाओं की भाँति उनकी रक्षा की जा सकती है। लेकिन स्वभावतः वह लड़ाकों की श्रेणी में ही गिना जाएगा और ग़ैर-लड़ाकों के अधिकार उसे छूट के तौर पर ही दिए जाएंगे। यह लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच अंतर का यही एक स्वाभाविक तरीक़ा है, और उन दो अतियों के बीच इसी एक मध्य बिंदु पर योद्धा और क़ानूनी समूहों की सहमति संभव ।
सेनानियों के अधिकार और दायित्व
ये दो प्रमुख वर्ग, अर्थात्, योद्धा और युद्धरत्त, अपने अधिकारों और दायित्वों के आधार पर विभिन्न क़ानूनों के अधीन हैं, इसलिए हम उन दोनों पर अलग-अलग चर्चा करेंगे। इनमें योद्धा/ लड़ाके/ सेनानी पहले स्थान पर हैं।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यूरोप में लड़ाकों के अधिकारों का सामान्य एहसास पहली बार उन्नीसवीं सदी के अंत में जाकर हुआ। यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से इनकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी थी और कुछ अधिकारों को व्यवहारिक जगत में सामूहिक चेतना के विकास के साथ-साथ मान्यता भी मिल चुकी थी, परन्तु इन अधिकारों की पूर्ण मान्यता बहुत बाद में प्रारम्भ हुई। 1829 तक, राज्य इस मामले पर किसी भी निश्चित क़ानून को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और ख़ुद को इस निर्णय का मुख़्तार समझते थे कि वे किन योद्धाओं को योद्धा के अधिकार प्रदान करेंगे और किन योद्धाओं को नहीं। अमेरिकी गृहयुद्ध में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि:
“एक राष्ट्र ख़ुद तय करेगा कि कब वह युद्ध कर रहे लोगों को लड़ाकों के अधिकार दे, चाहे युद्ध कर रहे वे लोग उसी राष्ट्र से हों जो ख़ुद को एक ऐसी सरकार से मुक्त कराना चाहता है जिसे वह दमनकारी समझता है या वह एक स्वतंत्र राष्ट्र हो और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हों।” (पार्लियामेंट्री पेपर्स एन. अमेरिका (1872) नं. 29, पृ.17)
लेकिन प्रत्येक राष्ट्र का अपनी कार्रवाइयों के लिए जज बन जाना किसी भी स्थिति में परिभाषित अधिकारों और दायित्वों का निर्माण नहीं कर सकता है, और व्यवहार में, इसका एकमात्र परिणाम यह हो सकता है कि युद्ध के लोगों के अधिकार और दायित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम के लोगों को अंततः इस कठिनाई का एहसास हुआ और धीरे-धीरे इस सिद्धांत को मान्यता मिली कि लड़ाकों को हर स्थिति में उनके अधिकार दिए जाएंगे।
1868 इसका प्रारंभिक नियम बनाया गया था। उसके कुछ वर्षों बाद, ब्रुसेल्स के सम्मेलन में कुछ अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्नीसवीं सदी के अंत तक इस विषय पर ऐसा कोई क़ानून नहीं बन सका जिसे सभी पश्चिमी शक्तियों ने मान्यता दी हो। सदी के अंत में जब पहला हेग सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसने व्यापक सिद्धांत निर्धारित किया था कि:
“लड़ाकों का एक दूसरे को नुक़सान पहुंचाने के साधनों का उपयोग करने का अधिकार असीमित नहीं है।”(हेग रेगुलेशन आर्ट. 22)
साथ ही, उसने लड़ाकों के अधिकारों और दायित्वों को भी परिभाषित किया, जो हेग विनियमों के अनुच्छेद 23 में वर्णित हैं:
विशिष्ट समझौतों में निषिद्ध मामलों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मामले विशेष रूप से निषिद्ध हैं:
1. “ज़हर और ज़हरीले हथियार का प्रयोग करना
2. युद्धरत राष्ट्र या सेना के किसी भी व्यक्ति की धोखा से हत्या करना या घायल करना
3. ऐसे दुश्मन की हत्या करना या उसे घायल करना, जिसने अपने हथियारों को आत्मसमर्पण कर दिया हो
4. यह घोषणा करना कि कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी
5. अत्यधिक नुक़सान पहुंचाने वाले हथियारों या आग लगाने वाले पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग करना।
6. शांति ध्वज या दुश्मन के राष्ट्रीय ध्वज या सैन्य प्रतीक या जिनेवा सम्मेलनों द्वारा निर्धारित विशिष्ट चिह्नों का अनुचित प्रयोग
7. शत्रु की संपत्ति को नष्ट करना बिना इसके कि युद्ध की ज़रूरतों के आधार पर ऐसा करना अनिवार्य हो।”
इस संक्षिप्त कथन से यह ज्ञात हुआ कि लड़ाकों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण कब और कैसे किया गया। इसके बाद अब हम विशेष अधिकारों और दायित्वों का अलग-अलग उल्लेख करेंगे।
1. युद्ध के नियमों का पालन
लड़ाकों का सबसे बड़ा दायित्व, जिस पर सरकारें ज़ोर देती हैं, यह है कि वे सैन्य अनुशासन का पालन करें और युद्ध के नियमों का पालन करें। लगभग सभी राज्यों ने अनियमित युद्ध करने वाले योद्धाओं के अधिकारों को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। जर्मनी के क़ानून में इसके लिए न्यूनतम दस साल की जेल और अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौथे संशोधन की धारा 83 उन्हें समुद्री लुटेरों और डकैतों के रूप में वर्गीकृत करती है और उन अपराधियों ही के समान सज़ा का प्रावधान करती है। इन लोगों को लड़ाकों के अधिकार तो दूर बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित रखा गया है। इसलिए, 1899 के हेग सम्मेलन में, ब्रिटेन ने ज़ोर देकर कहा कि असभ्य और जंगली राष्ट्रों के ख़िलाफ़ डम डम गोलियों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लॉर्ड लैंसडाउन, जो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अपने भाषण में दृढ़ता से कहा था कि 1895 में चित्राल की लड़ाई में बर्बर दुश्मन की भीड़ को रोकने के लिए साधारण गोलियां विफल रही थीं और डम डम गोलियां उन लोगों को बहुत नुक़सान नहीं पहुंचातीं। ये वही डम-डम की गोलियां हैं, जिनका उल्लेख ही यूरोपवासियों की अंतरात्मा को झकझोर देता है, और जिसे कोई भी “सभ्य राष्ट्रों के ख़िलाफ़ उपयोग करने की सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अनियमित युद्ध लड़ने वाले “असभ्य” राष्ट्रों के ख़िलाफ़, इन अमानवीय हथियारों का उपयोग इतना आवश्यक और न्यायसंगत है कि एक सबसे सभ्य यूरोपियन राज्य हेग घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है और केवल तभी हस्ताक्षर करता है जब अनुबंध पक्षों के आंतरिक युद्धों तक सीमित कर दिसा जोता है।
2. शरण
लड़ाकों का पहला और मौलिक अधिकार यह है कि जब वे शत्रु से शांति मांगें तो उन्हें शांति प्रदान की जाए। सत्रहवीं शताब्दी तक यूरोप में शरण देने की पद्धति का अभाव था। अंग्रेज़ी गृहयुद्ध के दौरान, संसद ने आयरिश लोगों को शांति प्रदान करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक, सेनानियों को एक दूसरे को शरण देने से इंकार करने का अधिकार था। इसलिए, 1794 में, फ्रांसीसी सम्मेलन ने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज़ी सैनिकों को शरण नहीं दी जाएगी। लेकिन 19वीं सदी में लड़ने वाले आदमियों के अधिकार को मान्यता मिली कि जब वे शांति की मांग करें तो उन पर कोई हाथ न उठाया जाए और उन्हें युद्धबंदियों का अधिकार दिया जाए।
3. युद्धबंदी:
युद्धबंदियों के संबंध में यूरोपीय क़ानून बहुत व्यापक हैं। लेकिन प्रोफेसर मार्गन के अनुसार, उनकी पूर्णता का वास्तविक कारण यह है कि इस में सभी राज्यों के हित संयुक्त हैं। प्रत्येक राज्य अपने सैनिकों और अधिकारियों का आराम चाहता है, इसलिए वह केवल विनिमय के रूप में दुश्मन के सैनिकों और अधिकारियों को आराम प्रदान करने के लिए सहमत होता है।
लेकिन ये सभ्य क़ानून हाल के युग के उत्पाद हैं। यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी तक युद्धबंदियों को दास बनाने का प्रचलन था। ग्रोतियुस ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ईसाई राष्ट्रों को सलाह दी कि वे एक-दूसरे को ग़ुलामों के रूप में बेचने के बजाय अपने बंदियों को फिरौती के लेकर छोड़ दें। लेकिन एक सदी तक उनके सुझाव बेअसर रहे। 18 वीं शताब्दी की शुरुआत में, फिरौती की व्यवस्था और युद्ध में बंदियों का आदान-प्रदान शुरू किया गया था, और सदी के अंत तक राज्यों ने इसका अभ्यास करना जारी रखा। विनिमय और हितों के संबंध में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1780 की संधि में, एक सैनिक की क़ीमत एक पाउंड और एक मार्शल की क़ीमत 60 पाउंड या 60 सैनिकों पर निर्धारित की गई थी। 19वीं शताब्दी में, यूरोप ने हितों की व्यवस्था को त्याग दिया और केवल विनिमय की प्रणाली को बनाए रखा। लेकिन सभ्यता के उस युग में भी युद्धबंदियों को मारने का तरीक़ा बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। 1799 में यूरोप के महानतम जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने याफा की चार हज़ार तुर्की सेना को मौत के घाट उतार दिया, केवल इस लिए कि वह उन के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा सकता था। लगभग एक सदी बाद, पश्चिमी दुनिया में फिर से वही अपराध किया गया। 1896 में, क्यूबा के स्पेनिश कप्तान, जनरल वीलर ने युद्ध के क़ैदियों को विद्रोही घोषित कर दिया और उन्हें मार डाला, और हज़ारों निवासियों को पकड़ लिया और उन्हें इस तरह से क़ैद कर लिया कि वे मक्खियों और मच्छरों की तरह भूखे प्यासे मर गए।
तथ्य यह है कि युद्ध के क़ैदियों के संबंध में औपचारिक नियम 1874 के ब्रसेल्स सम्मेलन में तैयार किए गए। 1899 के हेग सम्मेलन ने उनकी पुष्टि की और 1907 के दूसरे हेग सम्मेलन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क़ानून बना दिया। ये नियम मेमोरेंडम नंबर 4 से जुड़े नियमों में पाए जाते हैं।
यदि इन नियमों को संहिता के विवरण से अलग करके सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि उन्होंने इस्लाम के स्थापित सिद्धांत में कुछ भी नहीं जोड़ा है। पश्चिमी क़ानून युद्ध के क़ैदियों को उतनी ही सुख-सुविधाएं देना चाहता है जितनी एक राज्य अपने सैनिकों और उसी स्तर के अधिकारियों को देता है। मगर मुहम्मद (सल्ल.) और उसके साथियों का व्यवहार यह है कि उन्होंने युद्ध के क़ैदियों को अपने से बेहतर खिलाया और उन्हें अपने से बेहतर कपड़े पहनाए। हालाँकि, दुश्मनों के यहां, मुस्लिम युद्धबंदियों को रोटी और कपड़ा जैसी चीज़ें तो दूर, उलटा शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं। पश्चिमी राज्य युद्धबंदियों पर होने वाले ख़र्च का एक बड़ा हिस्सा उनके ही लोगों से प्राप्त करते हैं। लेकिन इस्लाम ने अपना धन उन पर उस समय ख़र्च किया जब इस मामले में दुश्मन राज्यों के साथ कोई समझौता करने की कोई संभावना नहीं थी। पश्चिमी साम्राज्य उन्हें केवल बदले में रिहा करने को तैयार हैं, लेकिन इस्लाम ने अक्सर उन्हें बिना बदले के रिहा कर दिया है और इसे बेहतर समझा है।
हालांकि उनमें कुछ चीज़ें इस्लाम से बढ़कर भी नज़र आती हैं। लेकिन उनके बारे में कोई राय बनाने में इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि प्रत्येक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य के सैनिकों को ये सभी रियायतें देने के लिए इस समझ पर सहमत हो गया है कि इसी तरह की रियायतें उसके सैनिकों को भी दी जाएंगी। इसके विपरीत इस्लाम ने बिना किसी समझौते के युद्धबंदियों को ऐसी रियायतें दी थीं कि उसे अपने विरोधियों से कोई रियायत मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बद्र की लड़ाई के क़ैदियों पर उस समय एहसान किया था जब मक्का के क़ुरैश के क़ब्ज़े में बीसियों मुस्लिम क़ैदी तपती रेत पर लिटाए जा रहे थे। उस समय उनके साथ कोई समझौता संभव नहीं था। इसलिए युद्धबंदियों को अधिक से अधिक वही रियायतें दी जा सकती थीं जो इस्लाम ने दीं। लेकिन आज, जबकि उनके साथ समझौता करना संभव है, इस्लाम कभी भी पिछले क़ानूनों में वृद्धी करने से इंकार नहीं करेगा। वह मुसलमानों को ग़ैर-मुस्लिमों के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करने की अनुमति देता है जिसमें समानता के साथ विशेषाधिकारों का आदान-प्रदान किया जाता है।
4. घायल, बीमार और मृतक
सेना के घायल और बीमारों के लिए सत्रहवीं शताब्दी तक यूरोप में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। शायद सत्रहवीं शताब्दी में पहली बार युद्ध अस्पतालों की स्थापना और युद्ध के मैदान पर तत्काल सहायता के लिए चिकित्सकों और सर्जनों को रखना शुरू हुआ। लेकिन दुश्मनों के घायलों, बीमारों और उसके अस्पतालों और चिकित्सकों को सम्मान ओर सुरक्षा देने की कल्पना यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी तक नहीं थी। घायल और बीमार लोगों को अक्सर मार दिया जाता था और अक्सर बहुत क्षीण अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अस्पतालों को सैन्य हमले से छूट नहीं दी गई थी। चिकित्सकों और बीमारों की देखभाल करने वालों को युद्धबंदी माना जाता था और उन्हें सामान्य लड़ाकों की तरह क़ैद कर लिया जाता था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के विशेषज्ञ इस मुद्दे पर मतभेद रखते थे कि डॉक्टरों और बीमारों की देखभाल करने वालों को युद्धबंदी माना जाना चाहिए या नहीं। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे क़ानूनी बना दिया कि अगर दुश्मन के डॉक्टरों की सेवाओं की ज़रूरत हो, तो उन्हें पकड़ कर उनसे बलपूर्वक काम लिया जा सकता है। 1864 तक यूरोप घायलों और बीमारों और चिकित्सकों के संबंध में सभ्य क़ानूनों से परिचित नहीं था। पहली बार उन्हें इस सभ्यता का पता तब चला जब एक प्रसिद्ध स्विस मानवतावादी हेनरी डुनेंट (Henry Dunant) ने उन “सभ्य राष्ट्रों” के बर्बर कृत्यों पर चेतावनी देने के लिए एक दर्दनाक आवाज़ उठाई। जून, 1859 में फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रियाई सेना के बीच सोलफेरियो में एक महान युद्ध हुआ था, जिसमें अन्य बहुत सारे क्रूर व्यवहारों के अलावा घायलों के साथ ऐसा पाश्विक व्यवहार किया गया कि पूरे यूरोप में मानवता की सूक्ष्म भावनाएँ सक्रिय हो गईं। हेनरी डुनन ने 1862 में इस पर एक किताब प्रकाशित की, जिसने यूरोप के जनमत को इन अत्याचारों की समाप्ति के लिए राजी कर लिया। अक्टूबर 1863 में, स्विस सरकार ने जिनेवा में एक अनौपचारिक कांग्रेस आयोजित की, जिसमें यह विचार किया गया कि युद्ध में घायल और बीमारों की सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। इस कांग्रेस के सुझाव पर अगले वर्ष जिनेवा में एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और बहुत वाद-विवाद के बाद एक संधि तैयार की गई, जिस पर 22 अगस्त, 1864 को सभी राज्यों (संयुक्त राज्य को छोड़कर) द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में सैन्य अस्पतालों और कर्मचारियों को तटस्थ घोषित कर दिया गया। उन्हें युद्धबंदी बनाने या उनके अस्पतालों को शत्रुता का निशाना बनाने से रोक दिया गया। बीमारों और घायलों के इलाज और देखभाल के काम का विरोध करना निषिद्ध ठहरा दिया गया। इसमें घायलों और बीमारों से संबंधित हर चीज़ के लिए एक सफेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस के प्रतीक चिन्ह की का सुझाव दिया गया, ताकि उसे दूर से ही पहचाना जा सके और जिस चीज़ पर यह प्रतीक लगा हो, वह शत्रुता का लक्ष्य न हो। इसके साथ ही प्रत्येक युद्धरत पक्ष के लिए अनिवार्य किया गया कि अपने घायलों के साथ-साथ शत्रु के घायलों का भी इलाज कराए और इलाज के बाद उन्हें या तो उनसे युद्ध में फिर से भाग न लेने का वादा करके, रिहा करदे या युद्धबंदी के रूप में रोक ले। (लॉरेंस पृ.348)
यह समझौता कई मायनों में त्रुटिपूर्ण था। इसमें सब से बड़ी कमी यह थी कि इन क़ानूनों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध ठहराने की कोई सिफ़ारिश नहीं थी। इस कमी को पूरा करने के लिए, 1868 में जिनेवा में फिर से एक और सम्मेलन आयोजित किया गया और एक पूरक समझौता तैयार किया गया। लेकिन न तो राज्यों ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार किया और न ही समझौते की पुष्टि की, इसलिए दूसरा जिनेवा कन्वेंशन पूरी तरह से बेकार साबित हुआ।
1874 के ब्रुसेल्स सम्मेलन ने फिर से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसकी सिफ़ारिशों का हश्र दूसरे जिनेवा सम्मेलन के समान ही हुआ। अंत मे 1906 में उसे स्वीकृति मिली। 4 जुलाई को एक समझौते तैयार किया गया जिसके आधार पर पश्चिमी राज्यों का क़ानून बना।
इसके बाद, 1907 के हेग कन्वेंशन ने उसी समझौते के आधार पर एक और समझौता किया जिसमें नौसैनिक युद्ध के लिए समान नियम लागू किए गए । लेकिन ब्रिटेन, इटली, ग्रीस, बुल्गारिया और सार्डिनिया सहित सम्मेलन में भाग लेने वाले 44 राज्यों ने इसकी पुष्टि नहीं की, इसलिए यह समझौता व्यावहारिक रूप से बेकार रहा। परिणाम यह हुआ कि 1914-18 के महायुद्ध में अस्पताली जहाज़ों को आज़ादी के साथ डूबाया गया।
इन सभी समझौतों का मूल सिद्धांत केवल एक है, और वह यह है कि जो दुश्मन युद्ध से अपंग हो चुका हो, या चोट या बीमारी ने उसे बेकार कर दिया हो, उस को किसी भी प्रकार का नुक़सान पहुँचाना मानवता के विरुद्ध है। इसी मूल से वे नियम निकलते हैं, जो अस्पतालों और उनके कर्मचारियों से संबंधित जिनेवा और हेग सम्मेलनों में निर्धारित किए गए हैं। देखने वाली एकमात्र चीज़ सिद्धांत है, तो पश्चिमी दुनिया ने आज उसकी खोज की है, लेकिन इस्लाम सदियों पहले इसे निर्धारित कर चुका है। अंतर यह भी है कि पश्चिमी दुनिया ने इसका निर्धारण तब किया जब सभी शक्तियां इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गईं, मगर इस्लाम ने इस सिद्धांत को युद्ध के अपने स्थायी क़ानूनों में उस समय शामिल किया जब ग़ैर-मुस्लिम दुनिया उससे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। लड़ाइयों में घायल मुसलमानों की अंधाधुंध हत्या कर दी जाती थी। ऐसे समय में, इस्लाम ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि तुम दूसरे पक्ष के अच्छे या बुरे व्यवहार की अनदेखी करते हुए अपने व्यक्तिगत दायित्व के तौर पर घायलों पर दया करो और उन सभी पर जो घायलों की तरह हैं।
5. घातक पदार्थों का उपयोग
जब से आधुनिक विज्ञान ने युद्ध के लिए नए-नए घातक हथियारों का आविष्कार करना शुरू किया है, तब से यूरोप में एक समस्या यह पैदा हो गई है कि इन घातक हथियारों, जहरीली गैसों, विस्फोटक पदार्थों और ऐसी अन्य चीज़ों के उपयोग को रोक दिया जाए। ये चीज़ें मानव शरीर पर, जो भयानक प्रभाव डालती हैं। उन्हें देखकर यूरोप की अंतरात्मा धिक्कारने लगती है। मानवतावादी जनमत को तैयार करके सत्ताधारियों पर दबाव डालते हैं कि युद्ध में ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग न करें। लेकिन इन चीज़ों से युद्ध के उद्देश्यों को हासिल करने में मिलने वाली मदद के कारण सैन्य दल इनका इस्तेमाल बंद करने को राजी नहीं है। दोनों गुटों में लंबे समय से खींचतान चल रही है। और इसका उपाय राजनीतिक विचारकों ने यह सोचा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके और उनमें मानवता पर घोषणापत्र तैयार करके नैतिकतावादियों को संतुष्ट कर देते हैं, और सैन्य समूह को स्वतंत्रता के साथ न केवल इन सभी चीज़ों के उपयोग की अनुमति दे देते हैं, बल्कि ऐसी अन्य नई चीज़ों के आविष्कार और अभ्यास की अनुमति भी दे देते हैं।
इस मामले में इस्लामी क़ानून ने किसी तरह का कोई विनिर्देश नहीं बनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी विशेष प्रकार के हथियार या गोला-बारूद के इस्तेमाल पर रोक सेनानियों की आपसी सहमति पर निर्भर करती है। अगर एक पक्ष किसी घातक पदार्थ का उपयोग करता है, तो दूसरे पक्ष के लिए उस पदार्थ का उपयोग न करना असंभव है। उस पर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध लगाना उसकी हार का पहले से फ़ैसला करने जैसा है। इसलिए, इस्लाम ने मुसलमानों को ऐसे सभी हथियार और युद्ध के तरीक़े अपनाने की अनुमति दी है जो उनके समय में प्रचलित हों और उन्हें अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध से जुड़ा कोई समझौता करने के मामले में भी स्वतंत्र छोड़ दिया है।
6. जासूस / गुप्तचर
जासूस किसी भी क़ानून द्वारा संरक्षित नहीं है। अन्य क़ानूनों की तरह, पश्चिमी क़ानून, भी इसे मान्यता नहीं देता। जासूस को केवल यह छूट दी गई है कि उसे मुकदमा चलाए बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। उसे दूसरी छूट यह दी गई है कि अगर वह जासूसी करके अपनी सेना में वापस लौट आता है और बाद में गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे पहले अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। इन प्रावधानों के साथ, हेग विनियम सैन्य अधिकारियों को यह अधिकार देते हैं कि वे जासूसी के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को जैसे चाहें दंडित करें।
इस मामले में इस्लामी क़ानून भी पश्चिमी क़ानून से अलग नहीं है। दोनों केवल शत्रु देश के उस यक्ति को जासूस ठहराते हैं जो दुश्मन के इलाक़े में घुस कर उसके रहस्यों की टोह में रहता है। जो व्यक्ति बिना किसी धोखे के खुलेआम दुश्मन की स्थिति का पता लगाने जाता है, उसे दोनों ही जासूस नहीं मानते हैं। हालाँकि, इस्लामी क़ानून जासूस को वे छूट नहीं देता जो पश्चिमी क़ानून उसे देता है। अस्ल में ये रियायतें ऐसी हैं जो दोनों पक्ष आपसी समझौते से एक-दूसरे के गुप्तचरों को देते हैं। चूँकि सभी राज्य जासूसों को नियुक्त करते हैं और कोई भी राज्य इन को दुश्मन की दया पर नहीं छोड़ना चाहता है,इस लिए उन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं। अगर ये रियायतें इस्लामी राज्य के गुप्तचरों को प्राप्त हों तो इस्लाम भी दुश्मनों के गुप्तचरों को ऐसी रियायतें दे सकता है।
7. युद्ध में चालबाज़ी
घात में रहना, दुश्मन को अनजाने में ख़तरे की जगह पर खींच लाना, उसे ग़लत सूचना देकर धोखा देना, आगे बढ़ने और पीछे हटने का नाटक करके, उसे गुमराह करना और फिर अचानक उस पर हमला कर देना । ऐसी और दूसरी चालें युद्ध में जायज़ हैं? इसके विपरीत दुश्मन को खतरे का संकेत दिखाकर पास बुलाना और उस पर हमला कर देना, शांति वार्ता के बहाने सफ़ेद झंडा उठाना और फिर उस पर टूट पड़ना, सैनिकों और हथियारों के शिविरों पर अस्पतालों के झंडे लगाना, महिलाओं और बच्चों को आगे रखना और उन के पीछे से गोली चलाना, और इसी तरह के अन्य कार्य, धोखा हैं, और किसी भी सेना के लिए ऐसा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर कहा नहीं जा सकता कि वे चाल में शामिल हैं या धोखेबाज़ी में। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के विद्वानों द्वारा दुश्मन के राष्ट्रीय ध्वज या उसकी सैन्य वर्दी के उपयोग की अनुमति है, लेकिन सैन्य दल इसको नाजायज़ ठहराता है। यह जर्मन क़ानून के तहत युद्ध का एक निषिद्ध रूप है, और अमेरिकी युद्ध क़ानून इसे ऐसी “बेईमानी” के रूप में परिभाषित करता है जो दुश्मन को किसी रियायत का हक़दार नहीं रहने देता है। अतः वास्तव में चाल और धोखे के संबंध में ऐसा कोई क़ानून नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें सभी विवरण मौजूद हो। यह प्रश्न एक राष्ट्र की सैन्य नैतिकता से संबंधित है और प्रत्येक राष्ट्र अपने सम्मान की भावना के आधार पर स्वयं निर्णय ले सकता है कि कौन से कार्य उनके साहस और बहादुरी के विरुद्ध हैं और कौन से नहीं। इसीलिए हेग के नियमों में (Ruses of war) धोखे और चाल की कोई व्याख्या नहीं दी गई और केवल यह लिखा गया कि दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साधनों का उपयोग जायज़ है।
इस्लाम का क़ानून इस मामले में भी पश्चिम के क़ानून से सहमत है। उसने भी Ruses of war को सही ठहराया है और इसके विवरण को समय की परिस्थितियों के अनुसार तय करने के लिए न्यायविदों पर छोड़ दिया है कि कौन सी चीज़ें धोखे की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी नहीं।
8. बदले की कार्रवाइयां
पश्चिमी साम्राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी क़ानून हमें यह नहीं बताता है कि दुश्मन द्वारा अतिचार होने पर हमें बदला लेने की अनुमति है या नहीं। और अगर है तो किस हद तक? हेग सम्मेलनों में शायद जानबूझकर इस मुद्दे को चर्चा से बाहर रखा गया है, क्योंकि सैन्य समूह इससे जुड़े सभी अधिकार अपने हाथों में रखना चाहता है। व्यक्तिगत रूप से, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के कुछ विशेषज्ञों ने इसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से, प्रो. हॉलैंड द्वारा प्रस्तावित सीमाएं क़ानूनी समूहों में बहुत लोकप्रिय हैं:
1. जिस अपराध का बदला लिया जाना है, उसकी पहले गहन छानबीन की जानी चाहिए।
2. उस अपराध से होने वाले नुक़सान की भरपाई किसी और तरीक़े से संभव न हो और असली अपराधी को सज़ा दिला पाना संभव न हो।
3. कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जवाबी कार्रवाई सेना के सर्वोच्च कमांडर की अनुमति से की जानी चाहिए।
4 बदला किसी भी सूरत में वास्तविक अपराध से बड़ा न हो।
लेकिन ये सभी न्यायविदों के निजी विचार हैं जिन्हें युद्धरत गुट ने कभी मान्यता नहीं दी। महायुद्ध के अनुभव से पता चलता है कि इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन यह है कि एक पक्ष द्वारा की गई हर कार्रवाई दूसरे पक्ष की उसी तरह की कार्वाइयों को जायज़ कर देती है। उदाहरण के लिए, युद्ध के क़ानूनों के तहत युद्ध के क़ैदियों को यातना देना, अस्पताल जहाज़ों पर हमला करना, व्यापारिक जहाज़ों को डूबाना, रक्षाहीन आबादी पर गोलाबारी करना, जहरीली गैस और विस्फोटक गोले का उपयोग करना अवैध है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में प्रत्येक पार्टी ने ये सभी कार्य किए यह कहकर कि दूसरा पक्ष भी ऐसा कर चुका है।
इस मुद्दे पर इस्लाम का क़ानून बहुत स्पष्ट है। वह कहता है:
وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍۢ سَيِّئَةٌۭ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ۔ (الشوریٰ :۴۰)
“बुराई का बदला उसी के जैसा बुरा है, और जो क्षमा कर देता है और सुधार करे तो उसका इनाम अल्लाह के ज़िम्मे है, क्योंकि वह अत्याचारियों को पसंद नहीं करता है।” (अल-शूरा: 40)
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌۭ لِّلصَّـٰبِرِينَ۔ (النحل : ۱۲۶)
“और यदि तुम लोग बदला लो, तो उतना ही लो, जितना तुम्हें सताया गया हो और यदि सब्र करो,, तो सब्र करने वालों के लिए ज़्यादा उत्तम है।”(अल-नहल: 126)
قِصَاصٌۭ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (البقرہ : ۱۹۴)
“जो कोई तुम पर ज़ुल्म करे तो तुम भी उसपर ज़ुल्म करो, जैसा कि उसने किया है, लेकिन अल्लाह से डरते रहो। और जान लो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है।” (अल-बकराः 194)
وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (البقرہ :١٩٠)
“तथा अल्लाह की राह में, उनसे युद्ध करो, जो तुमसे युद्ध करते हों, और ज़्यादती न करो, क्योंकि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता।” (अल-बकरा: 190)।
इन आयतों में, बदला न लेने और धैर्य रखने को बेहतर बताया गया है। और मजबूरी की हालत में बदला लेने की अनुमति दी गई है तो उसी हद तक जितनी ज़्यादती हुई है। फिर इस पर भी ज़ोर दिया गया है कि बदला लेने में परहेज़गारी करनी चाहिए और किसी भी सूरत में शरीयत की हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। परहेज़गारी और मर्यादाओं का पालन करने का अर्थ यह है कि किसी भी हालत में हराम और नाजायज़ काम नहीं किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर दुश्मन के सैनिक हमारे देश में घुस कर हमारी औरतों को अपवित्र करते हैं या मारे गए लोगों का अंग भंग करते हैं तो बदले में उनकी औरतों के साथ व्यभिचार करने और उनके मारे गए लोगों के अंग भंग करने की अनुमति नहीं है। या, उदाहरण के लिए, अगर वे युद्ध के दौरान हमारी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, घायल और बीमार लोगों की हत्या करते हैं, तो हमें बदले में ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर वे हमारे ख़िलाफ़ जहरीली गैसों का इस्तेमाल करते हैं या हम पर विस्फोटक बम फेंकते हैं, तो हमें उनके ख़िलाफ़ उसी शक्ति और विशेषताओं के हथियारों का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है।
ग़ैर-लड़ाकों के अधिकार और दायित्व
लड़ाकों के आपसी मामलों का उल्लेख करने के बाद, अब हम अपना ध्यान उन क़ानूनों की ओर मोड़ते हैं जो लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के आपसी मामलों से संबंधित हैं।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यूरोप में ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों का एहसास बहुत बाद में हुआ। सैद्धांतिक रूप से, यह अठारहवीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन व्यवहार में, उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक, युद्ध का कोई क़ानून नहीं था जो उन्हें लड़ाकों से अलग करने पर ज़ोर देता हो। अल्जीरिया में फ्रांस ने, 1857 की क्रांति में दिल्ली में इंगलैंड ने, और प्रायद्वीपीय युद्ध में सहयोगी सेनाओं ने, जिस स्वतंत्रता के साथ ग़ैर-लड़ाकों का नरसंहार किया, उससे पाश्विक युगीन भयावहता की याद ताज़ा हो गई।क़ानूनी विद्वान ग्रोटियस के समय से ही उनके अधिकारों के निर्धारण पर ज़ोर दिया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में यह कार्य पहली बार 1874 में ब्रुसेल्स कांफ्रेंस में शुरू किया गया। 1899 के हेग कांफ्रेंस ने इसे औपचारिक रूप दिया। और 1907 के हेग कन्वेंशन ने इसे पूरा किया। अत: अयोद्धाओं के संबंध में पाश्चात्य सभ्यता के विधान की आयु बहुत कम है।
इस क़ानून ने ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों और दायित्वों को बहुत व्यापक पैमाने पर निर्धारित किया है, और विवरण और शाखाओं के कवरेज में बहुत व्यापक रूप से काम किया है, लेकिन साथ ही यूरोप में युद्ध के जो आधुनिक तरीक़े और सिद्धांत बनाए गए हैं, उनके बाद, सेनानियों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच अंतर करना असंभव हो गया है, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ग़ैर-लड़ाकों के पक्ष में आज का युद्ध पाश्विक युग के युद्ध से अधिक ख़तरनाक है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन क़ानूनों पर ये भेद आधारित हैं, वे बहुत ही कमज़ोर और निराधार हैं।
लेकिन इसके वास्तविक कारण कुछ और हैं, जिन्हें प्रोफेसर ओपेनहाइम ने अपनी विद्वतापूर्ण किताब “इंटरनेशनल लॉ” में समझाया है। उनके शोध के अनुसार वर्तमान युग के युद्ध में लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों के बीच के अंतर को मिटाने का कारण चार बातों में छिपा है:
(1)। ज़बरदस्ती सैन्य भर्ती की घोषणा और एक राष्ट्र की पूरी आबादी को युद्ध सेवा में इस तरह से झोंक देना कि सक्षम लोग मैदान में चले जाएं और उनकी जगह महिलाओं और कमज़ोर पुरुषों को युद्ध की आपूर्ति करने और अन्य दायित्वों का पालन करने में लगाया जाए।
(2) हवाई जहाज़ों का उपयोग जो केवल किलों और दुर्गों को नष्ट करने के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि संचार और परिवहन के साधनों को भी नष्ट करने के लिए किया जाता है।
(3)। लोकतांत्रिक सरकारों की उन लोगों की राय के पालन से मुक्ति जो वास्तव में उन्हें चुनते हैं।
(4) दुश्मन पर आर्थिक दबाव डालने और उसके संसाधनों को बर्बाद करने का सामरिक महत्व।
अत:, वर्तमान समय के “सभ्य” युद्ध में ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होने का कारण केवल यह नहीं है कि युद्ध के पश्चिमी क़ानून कमज़ोर हैं, बल्कि वास्तविक कारण यह है कि इस समय के युद्ध जिन साधनों और तरीक़ों से लड़े जाते हैं, उनके बीच ग़ैर-लड़ाकों को लड़ाकों से अलग करना और उनके विशिष्ट अधिकारों का सम्मान करना असंभव हो गया है। इसके बावजूद, हमें यह देखना चाहिए कि पश्चिमी क़ानून ने ग़ैर-लड़ाकों के लिए क्या अधिकार और दायित्व निर्धारित किए हैं और उनका स्वयं क्या मूल्य है।
ग़ैर-लड़ाकों का पहला दायित्व
ग़ैर-लड़ाकों का पहला दायित्व यह है कि वे युद्ध में कोई हिस्सा न लें। जब दुश्मन उनके सामने आ जाए, तो उन्हें तय करना होगा कि उन्हें लड़ाई में भाग लेना है या नहीं। अगर वे युद्ध में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें नियमित रूप से अपनी राष्ट्रीय सेना में शामिल होना चाहिए, और अगर वे भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें शांतिपूर्वक अपने व्यवसाय में लगे रहना चाहिए। उनमें से जो किसी एक बात का फ़ैसला नहीं करेंगे और युद्ध में अनियमित तरीक़े से भाग लेंगे, उन्हें युद्ध के पश्चिमी क़ानूनों के अनुसार न लड़ाकों के अधिकार मिलेंगे और न ग़ैर-लड़ाकों के। अर्थात्, उनके साथ दया का व्यवहार नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी, और अगर उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो उन्हें युद्धबंदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
इस मुद्दे पर, इस्लामी क़ानून अंतरराष्ट्रीय क़ानून से इस हद तक सहमत है कि युद्ध में भाग लेने वाले ग़ैर-लड़ाकों को ग़ैर-लड़ाकों के लिए आरक्षित अधिकारों का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस्लाम इस बात से सहमत नहीं है कि उन्हें लड़ाकों का अधिकार भी नहीं दिया जाएं। इस्लाम हर लड़ने वाले को लड़ाकों का अधिकार देता है, लेकिन जब वे लड़ाई के साथ-साथ विश्वासघात और धोखा भी करते हैं, तो वह उन्हें कोई रियायत नहीं देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला चुपके से मुसलमानों के पानी में ज़हर मिला दे, तो वह निश्चित रूप से मारी जाएगी, या अगर कोई व्यक्ति मुसलमानों की शरण में आकर धोखे से उन्हें हानि पहुँचाता है, तो उसे अवश्य ही दंड दिया जाएगा। अक्कल और वरीना जनजाति के लोगों ने ऐसा ही किया था, कि वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शरण में आकर रहे और उनके चरवाहों को धोखे से मार डाला और ऊंटों को हांक ले गए। इसलिए पैग़म्बर (सल्ल.) ने उन्हें लड़ाकों और ग़ैर-लड़ाकों दोनों के अधिकारों से वंचित किया और उन्हें डाकू और लुटेरा ठहरा कर कड़ी सज़ा दी।
ग़ैर-लड़ाकों का यह भी दायित्व है कि जब दुश्मन सेना उनके क्षेत्र से गुज़र रही हो और उनसे मार्गदर्शन मांगे, तो वे उसका मार्गदर्शन करें और अगर वह परिवहन मांगे तो वे उसकी सेवा करें। युद्ध के उसके कार्यों में उसका विरोध न करें। अगर वे इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, तो आक्रमणकारी सेना को उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का अधिकार है।(लॉरेंस, पृ.345)
इस्लामी और पश्चिमी क़ानून इस मुद्दे पर सहमत हैं।
ग़ैर-लड़ाकों का सम्मान
इन दायित्वों के बदले, ग़ैर-लड़ाकों का मौलिक अधिकार यह है कि उन्हें युद्ध में मारे जाने से बचाया जाना चाहिए। यद्यपि युद्ध की स्थिति में, वे सेनाओं के हमले के निशाने पर आ जाएं। क़ानून के अनुसार आक्रमणकारी सेना का यह दायित्व है कि वह जानबूझकर अपने युद्ध संचालन को ग़ैर-लड़ाकों की ओर न मोड़े और जहाँ तक संभव हो उन्हें बचाने का प्रयास करे!
इस मामले में भी इस्लामी क़ानून और पश्चिमी क़ानून एक दूसरे से सहमत हैं। इस्लामी क़ानून ने ग़ैर-लड़ाकों पर जानबूझकर हमले पर रोक लगाई है, लेकिन युद्ध के दौरान अनजाने में उन पर हमला हो जाए तो उसपर कोई अभियोग नहीं है। अत: ताइफ की घेराबंदी में जब दुर्ग-रोधी उपकरणों का प्रयोग किया गया तो यह प्रश्न उठा कि नगर के ग़ैर-लड़ाकों को हानि पहुंचने की संभावना है। लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने उनके इस्तेमाल की इजाज़त इस आधार पर दी कि उसका मुख्य मक़सद दीवार को तोड़ना था, ग़ैर-लड़ाकों को निशाना बनाना नहीं था।
असुरक्षित आबादी पर गोलाबारी
ग़ैर-लड़ाकों के सुरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने के बाद, यह सवाल उठता है कि युद्ध की कार्रवाइयों खे दौरान इस अधिकार का सम्मान कैसे किया जाए। इस मुद्दे पर युद्धरत और क़ानूनी समूहों के बीच काफ़ी असहमति है, और अब क़ानूनी समूह की राय युद्धरत समूह की राय से पराजित हो रही है। अगर विरोधी सेनाओं के बीच आमने सामने का युद्ध हो, तो ग़ैर-लड़ाकों को तलवार से बचाया जा सकता है। लेकिन जहां मीलों दूर से गोलाबारी होती है और ख़ासकर जहां दुश्मन के किसी शहर को जीतने का इरादा हो, वहां ग़ैर-लड़ाकों को घातक युद्ध से सुरक्षित रखने की स्थिति क्या है?
इस सवाल का क़ानूनी समूह का जवाब है कि गोलाबारी के अधिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए. और युद्धरत गुट का कहना है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, ग़ैर-लड़ाकों को गोलाबारी से पहले शहर छोड़ने का समय देकर उनकी रक्षा करने की विधि तैयार की गई थी। 1870 के युद्ध में जर्मनी ने दो स्थानों पर इस प्रस्ताव का अनुपालन किया। लेकिन बाद में सैन्य समूह ने सर्वसम्मति से फ़ैसला किया कि इस तरह की राहत देना पूरी तरह से युद्ध के हितों के ख़िलाफ़ है।
इसलिए, जब जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर गोलाबारी शुरू की, तो उन्होंने ग़ैर-लड़ाकों को निकल जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस अवसर पर ग़ैर-लड़ाकों का शहर में मौजूद होना आवश्यक है, ताकि दुश्मन भुखमरी से घबराकर शहर हमारे हवाले कर दे।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि असुरक्षित आबादियों के लिए पश्चिमी क़ानून में जो अधिकार निर्धारित किए गए हैं वे एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं हैं। व्यवहार में पश्चिमी क़ानून इस एक विचार के सिवा कि “ग़ैर-लड़ाकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा होनी चाहिए।” अपने पास कुछ भी नहीं रखता।
विजित शहरों का आदेश
ग़ैर-लड़ाकों के अधिकारों पर बहस में एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब कोई शहर तलवार के बल पर पूरी तरह से जीत लिया जाए तो उस के निवासियों के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। प्राचीन काल में सेना का यह स्वाभाविक अधिकार था कि वह जिस शहर पर विजय प्राप्त करे उस शहर के निवासियों को मार डाले। यूरोप में भी निकट अतीत तक यह प्रचलन मौजूद था। स्पेन के ख़िलाफ़ संयुक्त नीदरलैंड के विद्रोह और उसके बाद हुए धार्मिक युद्धों में, समुदायों ने एक-दूसरे के शहरों पर स्वतंत्र रूप से आक्रमण किया और निवासियों का नरसंहार किया। हालाँकि तीस साल तक चले युद्ध के बाद, यूरोप की अंतरात्मा ने इस कृत्य को क्रूरता बताना शुरू किया, लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया था।
यूरोप में पहली बार इसे 1899 के हेग विनियम के अनुच्छेद 28 में निषिद्ध घोषित किया गया, जो विजित शहरों की लूटपाट और हिंसा पर रोक लगाता है। हालांकि व्यवहार में यह प्रचलन उस के बाद भी बंद नहीं हुआ। 1919 और 1920 में, यूरोप के सबसे सभ्य राज्यों के नेतृत्व में ग्रीक सैनिकों ने इज़मिर और थ्रेस में प्रवेश किया और ग़ैर-लड़ाकू नागरिक आबादी को तलपट कर दिया। यूरोप को आज तक विजित नगर में उस तरह प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, जो 14 सदी पूर्व मक्का विजय के अवसर पर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिस तरीक़ेम को इस्लाम के सच्चे ख़लीफ़ाओं ने इसे ईरान, इराक़, सीरिया, मिस्र और अफ्रीका के सैकड़ों शहरों की विजय के अवसर पर प्रदर्शित कर के दिखाया।
अनाधिकरण
अनाधिकरण (Occupation) एक आधुनिक शब्दावलि है और इसकी कल्पना भी आधुनिक है। प्राचीन काल में जब किसी राज्य पर किसी देश का अधिकार हो जाता था, तो वह देश उसका वैध अंग बन जाता था। इस्लामी क़ानून में, किसी देश की विजय का मतलब था कि वह दारुल-इस्लाम बन गया और उसकी प्रजा को ज़िम्मियों का अधिकार मिल गया। परन्तु आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार किसी राज्य या नगर पर शत्रु का क़ब्ज़ा हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि वह आधिकारिक रूप से उसके स्वामित्व में आ गया है। जब तक पूर्व सरकार से औपचारिक संधि के माध्यम से उस राज्य या नगर का स्वामित्व विजेता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तब तक वह उसके केवल प्रबंधन के अधीन रहता है। इसे “अनाधिकरण (Occupation)” शब्द में संदर्भित किया गया है। इस क़ब्ज़े वाले क्षेत्र के निवासी न तो व्यवहार में अपनी पिछली सरकार के नागरिक होते हैं और न ही सिद्धांत रूप में वे अपनी वर्तमान सरकार के नागरिक बनते हैं, बल्कि वे एक अवैध सैन्य सरकार के अधीन शोषण का शिकार होकर जीते हैं। 1899 और 1907 के हेग विनियमों ने इस शोषण की सीमाओं को निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया, और न ही यह निर्धारित किया कि क़ब्ज़ा करने वाली सरकार कि किस हद तक अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
हिंसा और उत्पात
सत्रहवीं शताब्दी तक, यूरोप में यह आम प्रथा थी कि जब कोई सेना दुश्मन के देश में प्रवेश करती, तो वह सब कुछ नष्ट कर देती थी। उस युग में शत्रुओं को लूटने और नष्ट करने का अधिकार असीमित था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक हमें इस अधिकार के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 1813 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा में कई गांवों को जला दिया और इसके जवाब में अंग्रेजों ने 1814 में वाशिंगटन की इमारतों को नष्ट कर दिया। 1837 में, फ्रांसीसी सैनिकों ने अल्जीरिया जम कर हिंसा और उत्पात मचाया। 1857 में, ब्रिटिश सैनिकों ने कानपुर, लखनऊ और दिल्ली क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आगज़नी, लूटपाट और हत्याएं कीं। क्रीमिया युद्ध से पहले रूस और तुर्की के बीच सभी लड़ाइयों में, तुर्की क्षेत्र में आगे बढ़ने पर रूसी सेना ने हमेशा आम तबाही मचाई। सत्रहवीं शताब्दी में सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस अधिकार को सीमित करने का विचार पैदा हुआ। उसके बाद, अठारहवीं शताब्दी में, वैटे ने नियम तैयार किया कि दुश्मन के देश में सामान्य विनाश की तीन अवस्थाएं जायज़ हैं:
(1) जबकि इसका उद्देश्य क्रूर और बर्बर शत्रु के बर्बर कृत्यों को रोकना है,
(2) जबकि अपनी सीमा रेखा को सुरक्षित करने के लिए रोक बनाने का इरादा है।
(3)। जबकि फील्ड मार्च या घेराबंदी के लिए इसकी ज़रूरत हो।
उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, पश्चिमी विचार ने सभ्यता की दिशा में कुछ और प्रगति की और इस सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया कि:
“विनाश की केवल उस सीमा तक अनुमति है जितना युद्ध की अनिवार्यता के संदर्भ में अपरिहार्य है।”
लेकिन 20वीं शताब्दी के यूरोपीय लेखकों और युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की ज़रूरतों के हिसाब से सभी प्रकार के विनाश की अनुमति है, लेकिन, केवल विनाश के उद्देश्य से किया जाने वाला विनाश निषिद्ध है।
जर्मन बुक ऑफ वॉर इस मुद्दे पर यह फ़ैसला देती है:
“अनावश्यक रूप से, थोड़ा सा विनाश भी नाजायज़ है, लेकिन अगर आवश्यक हो, तो बड़े से बड़ा विनाश भी जायज़ है।”
यहां आकर पश्चिमी क़ानून कुछ हद तक इस्लामी क़ानून से मिल जाता है। इस्लामी क़ानून में भी यही कहा गया है कि अगर किसी शहर पर विजय प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य सैन्य अभियान के लिए विनाश आवश्यक है, तो इसकी अनुमति है, लेकिन केवल उस हद तक जितना उस अभियान की सफलता के लिए अनिवार्य है।
तटस्थों के अधिकार और दायित्व
अब युद्ध के पश्चिमी क़ानूनों में से केवल एक ‘तटस्थता’ का नियम बचा है। इस पर टिप्पणी करने के बाद हम इस लंबे अध्याय को समाप्त कर देंगे।
पश्चिमी देशों में तटस्थता की अवधारणा बहुत हाल के युग की उपज है। दो सदी पहले तक उन्हें इसकी कोई अवधारणा नहीं थी, या अगर थी भी तो वह अधूरी थी। इसलिए इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए पश्चिमी भाषाओं में कोई शब्द नहीं था। ग्रोटियस ने इसे “मेडी” (Medii) शब्द से व्यक्त किया है और बिंकर्सच्वेक ने इसके लिए “नॉन होस्टेस” (Non Hostes) शब्द गढ़ा है। 17 वीं शताब्दी के अंत में, जर्मन और अंग्रेज़ी भाषाओं को पहली बार “न्युटरल” (तटस्थ) शब्द से परिचित कराया गया था।
यूरोप में सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों तक, तटस्थता को असंभव और ख़तरनाक माना जाता था, और वास्तव में इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं था। फिलारेस के दार्शनिक मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि जब उसके पड़ोसियों के बीच लड़ाई हो तो वह किसी एक पक्ष में शामिल हो जाए। एक सदी बाद, ग्रोटियस ने भी यह सलाह दी कि एक शासक को उस का पक्ष लेना चाहिए जिसे वह सही मानता हो, और जो ग़लत हो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जब उनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाए कि कौन सही है और कौन ग़लत, तब इस मामले में उसे दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंत तक, निष्पक्ष के अधिकार और विशेषाधिकार कुछ भी नहीं थे। युद्धरत्त ताक़तें लड़ते लड़ते बेधड़क उनकी सीमाओं में घुस जाते थे और तटस्थ शक्तियां उस पक्ष की मदद करने में संकोच नहीं करती थीं जिससे वे सहानुभूति रखते हैं। क़ानून के इस क्षेत्र में अधिकारों और दायित्वों और सीमाओं का निर्धारण 1794 में शुरू हुआ, जब अमेरिकी कांग्रेस ने पहली बार अमेरिकी नागरिकों को उन लोगों के साथ युद्ध में सेवा देने से रोक दिया जो संयुक्त राज्य सरकार के साथ युद्ध में नहीं थे। इसके बाद, इस क्षेत्र में क़ानून बनना लगातार जारी रहा, यहां तक कि 1818 में एक पूर्ण तटस्थता संहिता तैयार हो गई। 1819 में, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य के उदाहरण का अनुसरण किया और कांग्रेस द्वारा बनाए गए क़ानूनों को संविधान की अपनी किताब में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी उन क़ानूनों को अपनाया। उन्नीसवीं शताब्दी तक सभी पश्चिमी राज्यों में तटस्थता क़ानून बन गए। हालाँकि, तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय क़ानून सही अर्थों में 1907 के हेग सम्मेलन में तैयार किया गया था, क्योंकि यह पहली बार था कि पश्चिमी देशों ने संयुक्त रूप से तटस्थों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया था।
हेग कन्वेंशन 5 और 13 के अनुसार, भूमि और नौसैनिक युद्ध में तटस्थों के प्रति लड़ाका लोगों के दायित्व इस प्रकार हैं:
(1) तटस्थ राज्य की सीमाओं के भीतर कोई भी सैनिक कार्रवाई न की जाए।
(2) लड़ाका लोगों के लिए तटस्थ क्षेत्र के माध्यम से अपने युद्ध के सामान और सैनिकों आपूर्ति को ले कर जाना मना है।
(3) एक तटस्थ क्षेत्र को युद्ध की तैयारियों के लिए “आधार” नहीं बनाया जा सकता है।
(4) तटस्थ क्षेत्र या पानी में घुस कर दुश्मन को गिरफ़्तार करना या उस पर हमला करना तटस्थता के अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे बचना चाहिए।
(5) लढ़ाई करने वालों का दायित्व है कि एक तटस्थ साम्राज्य अपने तटस्थता के दायित्व को पूरा करने के लिए जो क़ानून बनाए उन क़ानूनों का पालन करें।
(6) अगर जाने-अनजाने किसी तटस्थ राज्य के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष का दायित्व है कि वह उसकी क्षतिपूर्ति करे।
इन सभी नियमों के पीछे सिद्धांत यही है कि एक तटस्थ राज्य की सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत इसी तरह इस्लाम में मौजूद है। इस्लामी क़ानून के स्थायी नियमों में से एक यह भी है कि जिस राष्ट्र के साथ इस्लामी राज्य की शांति-संधि हो, और जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेता है, उसकी सीमाओं पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अगर दुश्मन लड़ते लड़ते उसके क्षेत्र में जा पहुंचे, तो उसका पीछा नहीं किया जा सकता है। दुश्मन के जो लोग उसके देश में रह रहे हों उनपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। बल्कि, कुल मिलाकर युद्ध के दौरान, उसके लोगों के ख़िलाफ़ या उसके राज्य की सीमाओं से किसी भी तरह का आक्रमण बिल्कुल निषिद्ध (हराम) है।
वर्तमान काल में तटस्थों की स्थिति
यह एक विचित्र बात है कि बीसवीं शताब्दी में तटस्थता का नियम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा और फिर कुछ वर्षों में वह तोड़ डाला गया। दूसरे हेग कन्वेंशन को समाप्त हुए सात वर्ष भी नहीं हुए थे कि यूरोप में विश्व युद्ध छिड़ गया और इसने तटस्थता के पूरे क़ानून की धज्जियां उड़ा दीं। तटस्थता का कोई नियम ऐसा नहीं था, जिसका स्वतंत्रता के साथ हनन न हुआ हो। उनकी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया, उनके जहाज़ डुबाए गए, उनका व्यापार नष्ट किया गया, उनकी तलाशी ली गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, वह सब कुछ उनके साथ किया गया जो योद्धाओं के साथ किया जाता है। यह भी संदेहास्पद हो गया कि तटस्थों के पास वास्तव में कोई अधिकार था या नहीं। तब इतना ही नहीं तटस्थता की वास्तविकता भी काफ़ी हद तक संदिग्ध हो गई। चूंकि युद्ध अब केवल एक सैन्य युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि उस से अधिक एक आर्थिक युद्ध हो गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या वह शक्ति जो दुश्मन के साथ व्यापार करती है, उसकी ज़रूरतें पूरी करती है, और उसके आर्थिक जीवन को बनाए रखने में सहायक है। तो क्या यह वास्तव में तटस्थ है? क्या वह अपने लिए तटस्थता के अधिकारों की मांग कर सकती है?
इस मुद्दे ने तटस्थता की बुनियाद पर गहरा आघात किया है और यह सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय क़ानून अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि इन नई समस्याओं के आलोक में तटस्थों के दायित्व क्या निर्धारित करे और उन्हें क्या अधिकार दिलवाए।
समीक्षा
यह अध्याय अपेक्षा से अधिक लंबा हो गया है लेकिन समाप्त करने से पहले पिछली चर्चाओं पर एक अंतिम टिप्पणी करना आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि इस्लामी क़ानून किस तरह पश्चिमी क़ानून पर प्राथमिकता रखता है। अगर आपके दिमाग़ में पिछले पन्ने सुरक्षित हैं, तो चर्चाओं को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वरीयता के कारणों को इंगित करना पर्याप्त है।
पहली बात तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय क़ानून वास्तव में “क़ानून” ही नहीं है। यह अपने नियमों और विनियमों के संदर्भ में पूर्णतः राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। वे इसे जिस तरह चाहते हैं, उसे अपने स्वयं के हितों के अनुसार बनाते और बदलते हैं, और जो बात सभी या कुछ बड़े राज्यों को पसंद नहीं आती है, वह क़ानून में निहित नहीं रह सकती है। इस तरह, क़ानून वास्तव में यह तय नहीं करता है कि सरकारों का व्यवहार क्या होना चाहिए, बल्कि सरकारें ख़ुद तय करती हैं कि क़ानून क्या होना चाहिए।
इसके विपरीत, इस्लाम का क़ानून सही मायने में एक “क़ानून” है। यह एक उच्च शक्ति द्वारा बनाया गया है। मुसलमानों को इसे हटाने या संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यह केवल इसलिए तैयार किया गया है कि जो लोग इस्लाम का पालन करते हैं उन्हें निर्विवाद रूप से इसका पालन करना चाहिए, और जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें क़ानून तोड़ने वाला और अवज्ञाकारी ठहराया जाएगा। अगर पश्चिम के लोग अपने अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करते हैं, तो वह क़ानून ही नहीं रहता, लेकिन मुसलमान अगर सब मिलकर भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करें, तो भी इस्लामी क़ानून अपनी जगह क़ानून बना रहता है।
दूसरी बात यह कि युद्ध के क़ानून के रूप में जानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की शाखा वास्तव में अस्थायी और अत्यंत अविश्वसनीय है। युद्ध की ज़रूरतों के साथ उसका लगातार टकराव होता रहता है और हर बार वे ज़रूरतें क़ानून को पराजित करती रहती हैं। फिर सैन्य और क़ानूनी समूहों के बीच के मतभेद उसे और भी कमज़ोर कर देते हैं। क़ानूनी समूह कोई क़ानून बनाता है और सैन्य समूह उसे रद्द कर देता है। क़ानूनी समूह एक सभ्य नियम देता है और सैन्य समूह इसे स्वीकार करने से इंकार कर देता है। चूंकि कार्रवाई की सभी ताक़तें सैन्य समूह के हाथों में होती हैं, इस लिए किताबों में लिखा युद्ध का क़ानून किताबों में धरा रहता है और युद्ध का वास्तविक क़ानून वही होता है जो सेनाएँ स्वयं अपने कार्यों के माध्यम से युद्ध के मैदान में बनाती हैं। इसके विपरीत, युद्ध का इस्लामी क़ानून पूरे इस्लामी क़ानून की तरह एक दृढ़ और अपरिवर्तनीय क़ानून है। युद्ध से जुड़ी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो नियम-कायदे निर्धारित किए गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। किसी इस्लामी सेना या जनरल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह उसमें से कोई भी संशोधन कर सके या उसके किसी अंश को स्वीकार करने से इनकार कर दे।
तीसरी बात यह कि युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क़ानून लड़ने वालों की आपसी समझ पर आधारित है। कुछ राज्य मिलकर तय करते हैं कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो हम उक्त नियमों का पालन करेंगे। इस समझौते का हिस्सा नहीं होने वाले राष्ट्रों के साथ युद्ध की स्थिति में इस क़ानून का पालन नहीं किया जाएगा। उस समझौते से अलग होने वाले राष्ट्र भी इस क़ानून की सीमाओं से बाहर होंगे और वे अब सभ्य राष्ट्रों के सभ्य व्यवहार के हक़दार नहीं होंगे। यहां तक कि अगर समझौते में भाग लेने वालों में से कोई राज्य समझौते का उल्लंघन करता है, तो अन्य प्रतिभागियों को उसके ख़िलाफ़ युद्ध के क़ानूनों को अलग रखकर मनमानी करने की अनुमति होगी। आखिरकार, यह क़ानून तोड़ने वाला क़ानून ही बदल देता है। इस तरह यह क़ानून किसी नैतिक दायित्व की भावना पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल विनिमय और पारस्परिक हितों पर आधारित है। युद्ध का एक पक्षकार दूसरे के साथ सभ्य व्यवहार इस लिए नहीं करता कि उसे ऐसा करना चाहिए, बल्कि इस शर्त पर करता है कि अगर उसके साथ सभ्य व्यवहार किया जाता है, तो वह भी सभ्य व्यवहार करेगा, और अगर नहीं, तो वह नहीं करेगा। इस्लामी क़ानून इस तरह के समझौते पर आधारित नहीं है, इसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना मुसलमानों पर सभी परिस्थितियों में अनिवार्य है, चाहे ग़ैर-मुस्लिम बदले में उनके साथ शालीनता से व्यवहार करें या न करें। इस्लामी क़ानून किसी मुसलमान के इस अधिकार को मान्यता नहीं देता कि वह किसी परिस्थिति में उनके पालन से मुक्त हो जाए। जो भी मुसलमान रहना चाहता है उसे हर हाल में क़ानून की सर्वेच्यता स्वीकार करनी होगी।
चौथी बात यह कि पश्चिम के सभ्य क़ानूनों को अस्तित्व में आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि इस्लामी क़ानून चौदह सदियों से दुनिया में सभ्यता का झंडा ऊंचा किये हुए है। समय के इतने बड़े अंतर के बावजूद, जहां तक सिद्धांतों का संबंध है, पश्चिमी क़ानून ने इस्लामी क़ानून में एक अक्षर भी नहीं बढ़ाया है। अधिकांश पहलुओं में इस्लाम अभी भी पश्चिमी क़ानून से श्रेष्ठ है।
पांचवीं बात यह कि पाश्चात्य सभ्यता ने मनुष्य को कुछ व्यावहारिक नियमों से जोड़ कर स्वतंत्र छोड़ दिया है कि अपनी शक्ति को जहां चाहे, जैसे चाहे उपयोग करे।वह केवल यह अपेक्षा करती है कि जब वह किसी को मारे, तो इस तरीक़े से मारो, उस तरीक़े से न मारे। बाक़ी रहा यह सवाल कि किस उद्देश्य से मारे और किस उद्देश्य से न मारे, तो इससे उसे कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक इन सभ्य राष्ट्रों के कार्यों का संबंध है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता साम्राज्य विस्तार, व्यापार विस्तार, धन और भूमि के अधिग्रहण, जैसी सभी पाशविक इच्छाओं के लिए युद्ध की अनुमति देती है। इसके विपरीत, इस्लाम अपने अनुयायियों को लड़ने के केवल सभ्य तरीक़ों का पालन करने ही के लिए बाध्य नहीं करता है, बल्कि उन्हें यह भी बताता है कि तुम अमुक उद्देश्यों के लिए युद्ध लड़ सकते हो और अमुक उद्देश्यों के लिए नहीं लड़ सकते। उसने इस विषय को मनुष्य की व्यक्तिगत पसंद पर नहीं छोड़ा है, बल्कि उसे कुछ नैतिक सीमाओं में बाँध दिया है जिससे निकलने का उसे अधिकार नहीं दिया गया है।
यही कारण हैं जिनके आधार पर इस्लाम का युद्ध का क़ानून पश्चिम के क़ानून से अधिक सही, अधिक उपयोगी, अधिक उचित और अधिक मज़बूत है।
यहां यह आपत्ति की जा सकती है कि पश्चिम के मामले में तो आप पश्चिमी देशों के प्रचलन को देखते हैं, लेकिन इस्लाम के मामले में आप मुसलमानों के प्रचलन को नहीं देखते, बल्कि केवल इस्लामी क़ानून को देखते हैं। लेकिन पिछली चर्चाओं पर ग़ौर करने से यह आपत्ति स्वत: समाप्त हो जाती है। तथ्य यह है कि इस्लामी क़ानून और मुसलमानों का प्रचलन दो पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं। क़ानून बनाने में मुसलमानों के प्रचलन, या उनकी इच्छा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसलिए, जब क़ानून के गुणों और दोषों के बारे में चर्चा होती है, तो प्रचलन का प्रश्न स्वाभाविक रूप से चर्चा से बाहर हो जाता है। इसके विपरीत, पश्चिमी क़ानून और पश्चिमी देशों का प्रचलन दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। क़ानून बनाने में उन देशों के प्रचलन, और उनकी इच्छाओं का विशेष हस्तक्षेप है। ऊपर यह साबित किया जा चुका है कि जहां तक युद्ध के नियम का संबंध है, पश्चिमी देशों का प्रचलन आगे-आगे छलता है और क़ानून को उसका पालन करना पड़ता है। इसलिए, हम पश्चिम के मामले में उनके प्रचलन को देखने पर मजबूर हैं। अल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
(6) परिशिष्ट
सभ्य दुनिया युद्ध में सर्वथा असभ्य क्यों ?
परिचय
यह पुस्तकांश मौलाना सैयद अबुलआला मौदूदी की प्रसिद्ध पुस्तक "अल-जिहाद-फ़िल-इस्लाम" के परिशिष्ट के रूप में तैयार किया गया है। मौलाना मौदूदी ने वह किताब 1927 ई. में पूरी की। "अल-जिहाद-फ़िल-इस्लाम" के शीर्षक से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें इस्लाम में जिहाद की अवधारणा और उसकी स्थिति पर चर्चा की गई है, निस्संदेह, जिहाद भी इस पुस्तक में चर्चा का विषय है, लेकिन इस पुस्तक में कई अन्य विषयों पर भी सविस्तार चर्चा की गई है। मौलाना ने इस किताब में विभन्न धर्मों और सभ्यताओं में युद्ध की स्थिति की समीक्षा की है और इस्लाम में युद्ध की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण धर्मों और प्राचीन और आधुनिक परंपराओं में युद्ध की अवधारणा और उसकी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस किताब का आख़िरी अध्याय है, 'युद्ध आधुनिक सभ्यता में'। इस अध्याय में सैयद मौदूदी ने प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद किये गये शांति प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की है।
जब "अल-जिहाद-फ़िल-इस्लाम" के दूसरे संस्करण का समय आया, तब तक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी भी झेल चुकी थी, इसलिए मौलाना ने ज़रूरत महसूस की कि उस विश्व युद्ध और उसके बाद बनते-बिगड़ते हालात की समीक्षा करके किताब में शामिल कर दिया जाए। उन्ही दिनों मौलाना का स्वास्थ्य बिगड़ गया और दूसरा संस्करण बिना किसी परिवर्तन के प्रकाशित करना पड़ा। किताब में बाद की स्थितियों की समीक्षा जोड़ने की चिंता मौलाना के मन में लगातार बनी रही, लेकिन हालात हमेशा उन्हें अन्य कार्यों को प्राथमिकता देने पर मजबूर करते रहे। यहां तक कि 1979 में मौलाना की मृत्यु हो गई और वह काम बाक़ी ही रह गया।
अब जब इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने का निर्णय लिया गया, तो इसकी प्रसांगिकता बनाए रखने के लिए पुस्तक में परिशिष्ट के रूप में न केवल द्वितीय विश्व युद्ध, बल्कि पिछली एक शताब्दी के दौरान हुए वैश्विक परिवर्तनों का भरपूर सिंहावलोकन इसमें शामिल करने की आवश्यकता थी। यह पुस्तकांश उसी प्रयास का परिणाम है।
मूल पुस्तक में, मौलाना ने युद्ध के उद्देश्यों, युद्ध के नियमों, युद्ध की पद्धति और युद्ध की सीमाओं पर विशेष रूप से चर्चा की है और अन्य धर्मों और सभ्यताओं के साथ इस्लाम में युद्धों का इन्ही बिन्दुओं पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तकांश में भी द्वितीय विश्व युद्ध, से लेकर अब तक के प्रमुख युद्धों की समीक्षा इन्ही बिन्दुओं पर की गई है। विश्व स्तर पर चल रहे षड्यंत्रों और इस्लाम-विरोध को भी विषय बनाया गया है, क्योंकि इन दो कारकों ने कई एकतरफ़ा युद्धों को जन्म दिया है।
हिन्दी इस्लाम डॉट कॉम, 3 सितम्बर 223
विषय सूची
शीर्षक
परिचय
द्वितीय विश्व युद्ध (विस्तारवाद और अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन का परिणाम)
शीत युद्ध
क्रूरता और अन्याय का एक स्थायी अध्याय: फ़िलिस्तीन पर ज़ायोनी क़ब्ज़ा
कुत्सित प्रयासों की असफलता: वियतनाम युद्ध
आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध और अफ़ग़ानिस्तान पर हमला
तालिबान का असली चरित्र: एक क़ैदी की आपबीती
कमज़ोरी के अपराध की सज़ा : इराक़ पर अमेरिकी हमले
मानवता का अपमान: ग्वांतानामो बे और अबू ग़रीब
अंतर्राष्ट्रीय विवाद और संयुक्तराष्ट्र की भूमिका
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की दादागीरी
टकराव : सत्य और असत्य का या सभ्यताओं का ?
द्वितीय विश्व युद्ध
विस्तारवाद और अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन का परिणाम
1939 से 1945 तक दुनिया पर आच्छादित रहने वाला द्वितीय विश्व युद्ध (Second World war/ WWII) दुनिया का सबसे भयावह युद्ध था। इसका मुख्य कारण था सैन्यवाद और विस्तारवाद की प्रवृत्ति। इसे ग्लोबल वार या टोटल वार भी कहा जाता है। क्योंकि इस से पहले युद्ध सेनाओं के बीच होते थे, लेकिन इस युद्ध में नागरिकों को भी हताहत किया गया। निर्दोष नागरिक भी दुश्मन की हिंसक कार्रवाइयों का निशाना बन रहे थे और नागरिक-आबादियों पर हवाई हमले किए जा रहे थे। सबसे भयावह बात तो यह है कि इसी युद्ध में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में 61 देशों के लगभग एक अरब सैनिकों ने भाग लिया। इस युद्ध में 5 करोड़ नागरिक और 2।5 करोड़ सैनिक मारे गये। द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह दुनिया को दो भागों में बांटकर लड़ा गया था। एक ओर मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, पोलैंड, चीन, यूगोस्लाविया और ग्रीस शामिल थे। दूसरी ओर, धुरी राष्ट्र, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। 1 सितंबर 1939 को नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद ब्रिटेन और फ़्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चीन के ख़िलाफ़ जापानी सैन्यवाद, इथियोपिया के ख़िलाफ़ इतालवी आक्रामकता, और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रीय नियंत्रण को आपस में बांटने के लिए सोवियत संघ के साथ जर्मनी की साज़िश को युद्ध छिड़ने के कारणों के रूप में देखा जाता है।
हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बेशक, युद्ध शुरू करने के लिए हिटलर के विस्तारवाद और सैन्यवाद को ज़िम्मेदार माना जा सकता है, लेकिन अगर अन्य यूरोपीय सरकारें शांतिवादी और मानवता की हितैषी होतीं तो हिटलर की लगाई आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन अन्य देशों का रवैया, उनकी सोच और उनकी भूमिका भी किसी तरह हिटलर से कम नहीं थी। शांति बहाल करने की कोशिश करने के बजाय सभी देश युद्ध और हिंसा के जरिए अपने-अपने हित साधने में जुट गए। किसी को उत्पीड़ित देश का समर्थन करने में अपना हित नज़र आया, तो किसी ने अत्याचारी का साथ देने में ही भलाई देखी। शांति और मानवता से बेपरवाह, धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख देश एक-एक करके युद्ध में कूदते चले गए। नतीजा यह हुआ कि सात में से चार महादेश (यूरोप, एशिया, अफ्रीक़ा और उत्तर अमेरिका) इस महायुद्ध की आग में झुलस कर रह गये। आख़िरकार 6 साल बाद जब युद्ध की आग ठंडी हुई तो कोई भी देश अपने आप को विजेता कहने की स्थिति में नहीं था। प्रत्येक देश पराजित और क्षतिग्रस्त था। इस युद्ध में सबसे बढ़कर पराजय, अपमान और विनाश मानवता का हुआ, जिससे उसे हर तरह की हानि उठानी पड़ी। करीब साढ़े सात लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो बच गए उनमें से अनगिनत लोग शारीरिक रूप से घायल थे और बाकी सभी मानसिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा के शिकार थे। वित्तीय क्षति का हाल यह था कि कई स्थानों पर शहर के शहर नष्ट हो गए। वहां जो लोग बच गए थे, उनके पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए भोजन और न ही जीवन का कोई अन्य साधन।
द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण यूरोपीय देशों का जर्मनी के प्रति बुरा रवैया था। यूरोपीय देश अक्सर जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इनमें सबसे प्रमुख फ्रांस था, जो अक्सर जर्मनी को धमकी भी देता रहता था। 1919 में वर्साय की संधि में जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में उसकी भूमिका के लिए कड़ी फटकार लगाई गई और उसका उपहास उड़ाया गया। भविष्य में इसे सैन्य शक्ति बनने से रोकने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और भारी आर्थिक दंड भी थोप दिया गया। परिणामस्वरूप, जर्मन लोगों के बीच अन्य देशों के प्रति आक्रोश और तीव्र घृणा का एक सामान्य माहौल बन गया। कई लोगों ने वर्साय की संधि को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही, 1930 का दशक लोकतांत्रिक विफलता का दशक था। कई स्थानों पर लोकतंत्र बदनाम हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, दुनिया भर के देशों में निरंकुश तानाशाही पनपने लगी। इस स्थिति में, जर्मनी में राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वाकांक्षी नाजी पार्टी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ने लगी। 1933 में, पार्टी नेता एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी में अधिनायकवादी सत्ता संभाली। उन्होंने सबसे पहले वर्साय की संधि के प्रावधानों को ख़त्म करने का आह्वान किया और अपनी सेना को मज़बूत करना शुरू कर दिया। तानाशाह बनकर हिटलर ने अपने हवाई अड्डों और सेना को संगठित करना शुरू किया। हालांकि हिटलर स्वयं चुनाव जीतकर चांसलर बना था, लेकिन तानाशाह बनने के बाद उसने जर्मनी में चुनाव बंद करा दिये।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, इसलिए हिटलर जर्मनी को फिर से प्रतिष्ठा दिलाना चाहता था, इसके लिए उसने अपने दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली। हिटलर ने आक्रामक राष्ट्रवाद भड़काकर सभी जर्मनों को अपने पीछे एकजुट किया। उसने "मास्टर रेस" (सवर्ण) की दुहाई देकर जर्मनों और स्लावों को एकजुट करने की कोशिश की और पड़ोसी देशों में रहने वाले जर्मन मूल के लोगों को भी अपना समर्थक (भक्त) बना लिया। हिटलर की आक्रामक घरेलू और विदेश नीति, यहूदी विरोध, सैन्यवाद और विस्तारवाद ने कुछ ही वर्षों में खतरनाक रूप ले लिया।
प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अन्य कारकों में इथियोपिया और अल्बानिया के ख़िलाफ़ फासीवादी इटली की आक्रामकता और पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्सों पर शाही जापान की आक्रामकता शामिल थी। जिस तरह यूरोपीय देश प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेना बनाने में व्यस्त थे, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी सेना तैयार कर रहा था। जापान प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जापान ने अपनी सेना को मज़बूत करना शुरू कर दिया और साथ ही अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना और क़ब्ज़ा करना भी शुरू कर दिया। जापान लगातार अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण हुआ और धीरे-धीरे चीन के कई भागों पर कब्ज़ा हो गया।
इसी बीच जर्मनी, इटली और जापान के बीच समझौता हुआ कि युद्ध की स्थिति में तीनों एक-दूसरे का समर्थन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के कुछ क्षेत्र पोलैंड में मिला लिये गये थे और हिटलर उन पर पुनः कब्ज़ा करना चाहता था। लेकिन फ़्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड ने भी एक युद्ध समझौते पर हस्ताक्षर किये। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा करने का वादा किया। उसी वर्ष सोवियत संघ और जर्मनी ने संयुक्त रूप से पोलैंड पर आक्रमण की योजना बनाई।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया राष्ट्रसंघ चीन और इथियोपिया के सामने शक्तिहीन साबित हुआ। एक निर्णायक मौलिक घटना 1938 का म्यूनिख सम्मेलन था, जिसने औपचारिक रूप से जर्मनी के सुडेटनलैंड को चेकोस्लोवाकिया में शामिल करने को मंजूरी दे दी। मार्च 1938 में, जर्मनी ने प्रतिबंध के बावजूद, जर्मन आबादी वाले देश ऑस्ट्रिया पर क़ब्ज़ा कर लिया। 1938 में, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया (सुडेटनलैंड) में एक जर्मन क्षेत्र का दावा किया। म्यूनिख सम्मेलन में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों ने इस उम्मीद के साथ उस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के "हिटलर" के अधिकार को मान्यता दी कि "हिटलर" अब और किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा नहीं करेगा। लेकिन वादे के बावजूद, हिटलर ने 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा कर लिया। उसका अगला निशाना पोलैंड हो सकता था। हिटलर को इससे रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध की धमकी दे डाली। इसके बावजूद 1 सितंबर, 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसी समय फ्रांस और ब्रिटेन ने घोषणा की कि वे जर्मनी पर हमला करेंगे। इस प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
प्रथम विश्व युद्ध की विरासत
द्वितीय विश्व युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की विरासत के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा सभी पक्षों को संतुष्ट किए बिना ही कर दी गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में सभी महत्वपूर्ण निर्णय "बिग फोर" (ब्रिटेन के डैविड लॉयड जॉर्ज, इटली के विटोरियो इमानुएल ऑरलैंडो, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसौ, अमेरिका के वुडरो विल्सन) द्वारा किए गए थे। स्पष्ट है कि बिग फोर ने अपने हितों को प्राथमिकता दी और अन्य देशों के हितों की अनदेखी की, इस प्रकार कई देशों के भीतर असंतोष के रूप में एक व्यापक युद्ध के बीज बो दिए गए, जो माहौल के अनुकूल होते ही प्रस्फुटित होने लगे।
1918 के अंत में, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, दुनिया की आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ पूर्ण रूप से बदल गई थीं। मित्र राष्ट्र विजयी हुए, लेकिन यूरोप की अधिकांश अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया और, हमेशा की तरह, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। फ़्रांस, अन्य देशों के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक मनोबल के संबंध में हताश स्थिति में था, और समझता था कि 1918 में उसकी स्थिति "कृत्रिम और अस्थायी" थी। फ्रांस के प्रधान मंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसियो ने वर्साय की संधि के माध्यम से फ्रांस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया। इसी लिए, युद्ध का हर्जाना, कोयला भुगतान, फ्रांसीसी सुरक्षा की मांग, जैसे मुद्दे 1919-20 के पेरिस शांति सम्मेलन में छाए रहे।
प्रथम विश्व युद्ध शुरू करने के लिए जर्मनी को पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया गया था। "युद्ध अपराध धारा" जर्मनी के ख़िलाफ़ फ्रांस की जवाबी कार्रवाई में पहला कदम था। गेन्सबर्ग ने तर्क दिया कि युद्ध ने फ्रांस को इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसने बदला लेने और जर्मनी के फिर से शक्तिशाली बनने के डर से उसे अलग-थलग करना चाहा। हालाँकि, बीस साल बाद, नाजी आक्रमण और क़ब्ज़े के दौरान फ्रांस को अपने बदला की क़ीमत चुकानी पड़ी।
फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंडे की दो मुख्य वस्तुएँ जर्मनी से मुआवजे के रूप में धन और कोयले की वसूली और जर्मनी से राइनलैंड का कब्ज़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार लेने के अलावा, फ्रांसीसी सरकार ने मुद्रास्फीति के कारण धन की कमी की भरपाई के लिए अतिरिक्त मुद्रा छापी। फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जर्मनी से प्रतिबंध आवश्यक थे। फ्रांस ने यह भी मांग की कि युद्ध के दौरान फ्रांसीसी कोयला खदानों के विनाश की भरपाई के लिए जर्मनी फ्रांस को कोयले की आपूर्ति करे। फ्रांसीसियों ने कोयले की इतनी बड़ी रकम की मांग की जिसका भुगतान करना जर्मनी के लिए तकनीकी रूप से असंभव था।
फ़्रांस ने भविष्य में किसी भी जर्मन आक्रमण को रोकने की उम्मीद में जर्मनी से राइनलैंड को सौंपने पर भी ज़ोर दिया। कोयला भुगतान और असैन्यीकृत राइनलैंड सिद्धांत, जैसे अपूरणीय क्षति, को जर्मनों द्वारा अत्यधिक अपमानजनक और नाजायज़ माना जाता था।
वर्साय की संधि ने युद्ध का औपचारिक अंत तो कर दिया, लेकिन सभी पड़ोसी सरकारों द्वारा जर्मनी के ख़िलाफ़ लिया गया निर्णय न तो इतना सहज था कि जर्मनी उस पर सहमत हो जाता, और न ही इतना गंभीर था कि जर्मनी को पुनः महाद्वीप पर एक प्रमुख शक्ति बन कर उभरने से रोक पाता। जर्मन लोगों ने इस संधि की युद्ध अपराध के रूप में निंदा की और इसे दीर्घकालिक शांति का आश्वासन देने वाली संधि का पालन करने के बजाय उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी के लिए दंडित करने के रूप में देखा। इस समझौते के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विखंडन और बड़े पैमाने पर जातीय पुनर्वास हुआ, जिससे लाखों जातीय जर्मन पड़ोसी देशों से अलग हो गए।
ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के प्रयास में, वाइमर गणराज्य (जर्मनी) ने खरबों रुपये छापे, जिससे बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति बढ़ी। युद्ध के बाद की सरकारों के सामने सब से बड़ी समस्या भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ा जा रहा क़र्ज़ का बड़ा बोझ था। विजयी पक्ष को मुआवज़ा देना एक पारंपरिक सज़ा थी जिसके प्रचलन का एक लंबा इतिहास था, लेकिन जर्मनी के मामले में यह "बेहद अव्यवस्थित" था जिससे जर्मनों में नाराज़गी फैल गई। जर्मन जनता की नाराज़गी को अनुचित भी नहीं ठहराया जा सकता है। यह अति नहीं तो और क्या है कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 92 साल बाद 3 अक्टूबर, 2010 को अंतिम दंड राशि का भुगतान किया है।
राइनलैंड के विसैन्यीकरण और सेना में अतिरिक्त कटौती ने भी जर्मनों को नाराज़ कर दिया। यद्यपि यह तर्कसंगत है कि फ्रांस राइनलैंड को एक तटस्थ क्षेत्र बनाना चाहेगा, लेकिन फ्रांस की यह इच्छा केवल फ्रांसीसियों की नाराज़गी के बल पर निर्भर नहीं रह सकती थी। इसके अलावा, वर्साय की संधि ने जर्मन जनरल स्टाफ को भंग कर दिया और नौसैनिक जहाज़ों, विमानों, जहरीली गैस, टैंकों और भारी तोपखाने की ज़ब्ती को ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया। विजयी राष्ट्रों, विशेष रूप से फ्रांस द्वारा उनका समर्थन किए जाने, और उनकी मूल्यवान सेना छीन लिए जाने से, जर्मनों में आक्रोश भड़क उठा। ऑस्ट्रिया ने भी इस संधि को नाजायज़ पाया, जिससे हिटलर की लोकप्रियता बढ़ी।
इन शर्तों ने युद्धोन्मादियों के ख़िलाफ़ तीव्र आक्रोश पैदा किया, जिन्होंने जर्मन लोगों से वादा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के चौदह सूत्र शांति की ओर ले जायेंगे। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में केवल एक छोटी भूमिका निभाई और विल्सन मित्र राष्ट्रों को अपने चौदह सूत्री सिद्धांतों को अपनाने के लिए मनाने में असमर्थ रहे। कई जर्मनों ने महसूस किया कि जर्मन सरकार इस समझ के आधार पर युद्धविराम के लिए सहमत हो गई थी, जबकि अन्य लोगों को लगा कि 1918-1919 की जर्मन क्रांति "नवंबर के अपराधियों" द्वारा आयोजित की गई थी, जिन्होंने बाद में नए वाइमर गणराज्य में सत्ता संभाली थी। जापानियों ने भी वर्साय की संधि की बातचीत के दौरान उनके साथ हुए भेदभाव को लेकर पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रति नाराज़गी व्यक्त करना शुरू कर दिया। जापानियों द्वारा उठे गए नस्लीय समानता के मुद्दे को प्रस्ताव के अंतिम मसौदे में नहीं रखा गया था और मेज पर उस पर बमुश्किल ही कोई चर्चा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विरासत दोनों युद्धों के बीच बराबर बनी रही।
राष्ट्रसंघ की विफलता
लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन था। लीग के तरीकों में निरस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, देशों के बीच विवादों को बातचीत की कूटनीति के माध्यम से सुलझाना और वैश्विक कल्याण में सुधार करना शामिल था। लीग के पीछे का कूटनीतिक दर्शन पिछली शताब्दी की तुलना में विचारों में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। नए दर्शन ने निर्धारित किया कि लीग एक कानूनी निकाय के रूप में राष्ट्रों के बीच विवादों को निपटाने की भूमिका के साथ, सरकारों की सरकार के रूप में कार्य करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन लीग के मुख्य वास्तुकार थे। हालाँकि, संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट रूप से इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा कम हुई।
मूल रूप से, राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन था जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति तो थी, लेकिन उसे लागू करने की शक्ति नहीं थी। लीग के पास अपनी कोई सशस्त्र सेना नहीं थी, इसलिए उसे प्रस्तावों को लागू करने, आर्थिक प्रतिबंधों को बनाए रखने या ऐसी किसी अन्य आवश्यकता के लिए लीग के सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। सरकारें आम तौर पर किसी देश या देशों के ख़िलाफ़ अपनी सेना या बल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होती थीं। 1920 के दशक में कई उल्लेखनीय सफलताओं और कुछ प्रारंभिक विफलताओं के बाद, लीग अंततः 1930 के दशक में धुरी शक्तियों की आक्रामकता को रोकने में विफल रही। सर्वसम्मत निर्णयों पर निर्भरता, सशस्त्र बलों के स्वतंत्र संगठन की कमी और इसके प्रमुख सदस्यों के स्वार्थ ने लीग की विफलता को अवश्यमभावी बना दिया था।
विस्तारवाद और सैन्यवाद
विस्तारवाद आमतौर पर सैन्य आक्रामकता के माध्यम से किसी देश के क्षेत्रीय आधार (या आर्थिक प्रभाव) का विस्तार करने का सिद्धांत है। सैन्यवाद राष्ट्रीय हितों और/या मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से उपयोग की जाने वाली मज़बूत सैन्य क्षमताओं को प्राप्त करने की नीति है।
हालाँकि वर्साय की संधि और राष्ट्र संघ ने सभी उपायों से विस्तारवादी और सैन्यवादी नीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया की नई भू-राजनीतिक स्थिति में इन शर्तों को लागू करना मुश्किल था। अंतरयुद्ध काल के दौरान। 1930 के दशक की शुरुआत तक, जर्मनी, जापान और इटली में अत्यधिक सैन्यवादी और आक्रामक राष्ट्रीय विचारधारा प्रबल हो गई थी। इस अभ्यास ने सैन्य प्रौद्योगिकी, विध्वंसक प्रचार और अंततः क्षेत्रीय विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यह देखा गया है कि अचानक सैन्यीकृत देशों के नेताओं को यह साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है कि उनकी सेनाएँ मज़बूत हैं, इसलिए वे कमजोरों के ख़िलाफ़ अपनी आक्रामकता को उचित ठहराते हैं। इटालो-एबिसिनियन युद्ध और दूसरा चीन-जापानी युद्ध इसी प्रवृत्ति का परिणाम थे।
इटली में, बेनिटो मुसोलिनी ने भूमध्य सागर के आसपास केंद्रित एक नया रोमन साम्राज्य बनाने की कोशिश की। उसने 1935 की शुरुआत में इथियोपिया, 1938 की शुरुआत में अल्बानिया और बाद में ग्रीस पर हमला किया। उन्होंने राष्ट्र संघ की नाराज़गी और तेल प्रतिबंध को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।
नाजी शासन के तहत, जर्मनी ने ऐतिहासिक जर्मनी की "यथोचित" सीमाओं को बहाल करने का प्रयास करते हुए, विस्तार का अपना कार्यक्रम शुरू किया। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मार्च 1936 में राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण किया गया। एक वृहद जर्मनी का विचार भी महत्वपूर्ण था, जिसके समर्थकों का इरादा जर्मन लोगों को एक राष्ट्र-राज्य के तहत एकजुट करना था, जिसमें वे सभी क्षेत्र शामिल थे जहां जर्मन रहते थे, भले ही वे किसी विशेष क्षेत्र में अल्पसंख्यक हों। वर्साय की संधि के बाद, जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी के उत्तराधिकारी राज्य, नवगठित जर्मन-ऑस्ट्रिया के बीच एक संघ को मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, भले ही ऑस्ट्रिया के जर्मन बहुमत ने संघ का समर्थन किया था। परिणामस्वरूप, नाजी पार्टी में उग्र विचारधारा वाले व्यक्तियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। इसने, अपने नस्लीय आदर्शों के साथ मिलकर, अजेय भावना को बढ़ावा दिया और जर्मनी को अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया।
एशिया में, जापान के साम्राज्य ने मंचूरिया और चीन गणराज्य की ओर विस्तारवादी कदम उठाए। जापान में दो समकालीन कारकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी सेना की बढ़ती शक्ति और अराजकता दोनों में योगदान दिया। एक कैबिनेट कानून था, जिसके तहत इंपीरियल जापानी सेना (आईजेए) और इंपीरियल जापानी नौसेना (आईजेएन) में बदलाव करने से पहले कैबिनेट सदस्यों को नामांकित करना आवश्यक था। इसने अनिवार्य रूप से सेना को संसदीय देश में कोई भी कैबिनेट बनाने का अधिकार दे दिया। एक अन्य कारक गेकोकोजो, या कनिष्ठ अधिकारियों की ओर से संस्थागत अवज्ञा था। कट्टरपंथी कनिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने लक्ष्यों के रास्ते में आने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या करना आम बात थी। 1936 में, 26 फरवरी को कनिष्ठ अधिकारियों ने तख्तापलट का प्रयास किया और जापानी सरकार के प्रमुख सदस्यों की हत्या कर दी। 1930 के दशक में, महामंदी ने जापान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और जापानी सेना के भीतर कट्टरपंथी तत्वों को सेना को पूरे एशिया पर विजय के लिए काम करने के लिए मजबूर करने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए, 1931 में, क्वांटुंग सेना, (मंचूरिया में तैनात एक जापानी सैन्य बल) ने मकदान घटना का मंचन किया, जिसके कारण मंचूरिया पर आक्रमण हुआ और यह जापानी कठपुतली राज्य मंचुकुओ में बदल गया।
संसाधनों और बाज़ारों पर जापान का कब्ज़ा
सखालिन द्वीप पर कोयले और लौह अयस्क के कुछ भंडार और एक छोटे तेल क्षेत्र के अलावा, रणनीतिक खनिज संसाधनों की कमी है। 20वीं सदी के अंत में रुसो-जापानी युद्ध में, जापान कोरिया और मंचूरिया में रूसी साम्राज्य के पूर्वी एशियाई विस्तार से आगे निकलने में सक्षम था। 1931 के बाद जापान का लक्ष्य अधिकांश पूर्वी एशिया पर आर्थिक प्रभुत्व हासिल करना था, जिसे अक्सर एशियाई लोगों के लिए पैन-एशियाई शब्द में व्यक्त किया जाता था। अब जापान चीनी बाजार पर हावी होने के लिए दृढ़ था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व था। 19 अक्टूबर, 1939 को जापान में अमेरिकी राजदूत, जोसेफ सी ग्रोव ने अमेरिका-जापान सोसाइटी को एक आधिकारिक संबोधन में कहा: "पूर्वी एशिया में नए आदेश ने अन्य बातों के अलावा, चीन में अमेरिकियों को उनके लंबे समय से स्थापित अधिकारों से वंचित करने का खुलासा किया है, और अमेरिकी लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।" 1937 में, जापान ने मंचूरिया और चीन पर आक्रमण किया। ग्रेटर ईस्ट एशिया के समृद्ध क्षेत्र की आड़ में, “एशिया के लिए एशिया!” जैसे नारों के साथ जापान ने चीन में पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने और उसके स्थान पर जापानी आधिपत्य स्थापित करने की मांग की।
चीन में चल रहे विवाद के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान का यकराव शुरू हुआ, जहाँ नानकिंग नरसंहार और बढ़ती जापानी शक्ति जैसी घटनाओं ने जनता को भयभीत कर दिया। जब जापान फ्रांसीसी-इंडोचीन के दक्षिणी भाग में भी पहुंच गया, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका में सभी जापानी संपत्तियों को ज़ब्त करने का फ़ैसला किया। इसका उद्देश्य अमेरिका से जापान को तेल शिपमेंट में कटौती करना था, जो जापान के 80 प्रतिशत तेल आयात की आपूर्ति करता था। नीदरलैंड और ब्रिटेन ने भी इसका अनुसरण किया। तेल भंडार के साथ जो शांतिकाल के दौरान केवल डेढ़ साल तक चलेगा (युद्धकाल के दौरान बहुत कम), इस एबीसीडी लाइन ने जापान के सामने दो विकल्प छोड़े: चीनी वापसी की अमेरिकी नेतृत्व वाली मांग का अनुपालन करना या ईस्ट इंडीज में तेल क्षेत्रों को ज़ब्त करना। जापानी सरकार ने चीन से हटना स्वीकार्य समझा।
हिटलर की देखा-देखी इटली के मुसोलिनी ने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध की आशंकाएँ बढ़ने लगीं। अगस्त 1939 तक यूरोपीय शक्तियों का मानना था कि जर्मनी अपने महान शत्रु रूस से सीधे टकराव के डर से पोलैंड पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन यह विचार तब गलत साबित हुआ जब जर्मनी और रूस ने आपसी मित्रता की संधि की और तय किया कि वे पोलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे और उसे अपने बीच बांट लेंगे।
युद्ध की आधिकारिक शुरुआत
1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा कर दी (ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा करने से, उसके प्रभुत्व वाले देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और भारत न चाहते हुए भी युद्ध में शामिल हो गए।) इस प्रकार, 3 सितंबर, 1939 को यूरोप में आधिकारिक तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। पोलैंड के पूर्वी हिस्से पर क़ब्ज़ा करने के अलावा, रूस ने पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक राज्यों (लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया) को रूस में मिला लिया, लेकिन फिनलैंड ने उसका विरोध किया और उसने 1949 तक लड़ाई लड़ी।
ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद, दोनों पक्षों के बीच सात महीने तक लड़ाई अपेक्षाकृत कम रही। अप्रैल 1940 में, जर्मनी ने उत्तर में डेनमार्क और नॉर्वे पर अचानक हमला हमला करके क़ब्ज़ा कर लिया। (नॉर्वे का तट ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जर्मनी के लिए एक उत्कृष्ट नौसैनिक अड्डा था।) मई 1440 में पश्चिम में "हॉलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग" पर कब्ज़ा करने के बाद, जर्मनी ने 14 जून को पेरिस पर विजय प्राप्त की।
22 जून को फ़्रांस के आत्मसमर्पण के बाद, जर्मनी ने फ़्रांस के उत्तरी भाग पर सीधा नियंत्रण कर लिया, जबकि दक्षिणी भाग में "मार्शल पेटन" के नेतृत्व में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की। उनकी सरकार को "माध्यमिक" सरकार कहा जाता था। फ्रांस के पतन के बाद, जनरल डी गॉल ने लंदन में निर्वासित सरकार की स्थापना की और फ्रांस की पुनर्प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू किया। फ़्रांस के बाद "हिटलर" का अगला निशाना ब्रिटेन था, जहाँ "चेम्बरलेन" की जगह विंस्टन चर्चिल को प्रधान मंत्री बनाया गया।
जर्मन और ब्रिटिश हवाई युद्ध
13 अगस्त 1940 को जर्मनी ने ब्रिटेन पर हवाई हमला किया। शुरुआत में जर्मन वायु सेना ने ब्रिटिश हवाई अड्डों और कारखानों को निशाना बनाया, फिर 7 सितंबर से उनके शहरों पर बमबारी शुरू कर दी, लेकिन ब्रिटिश वायु सेना के मज़बूत प्रतिरोध के कारण 16 मई, 1941 को हिटलर ने यहां लड़ाई स्थगित कर दी और भूमध्य सागर (उत्तरी अफ्रीका) और पूर्वी यूरोप की ओर रुख कर दिया। भूमध्य सागर में हिटलर का मुख्य उद्देश्य अपने युद्ध सहयोगी "मुसोलिनी" का सहयोग करना था। युद्ध की शुरुआत में इटली तटस्थ था, लेकिन जर्मनी द्वारा फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद, मुसोलिनी फ्रांस और ब्रिटेन के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा करके जर्मनी का सहयोगी बन गया। 27 सितंबर को जर्मनी और इटली ने जापान को भी गठबंधन में शामिल कर लिया। उन्हें "अक्षीय/धुरी/एक्सिस शक्तियाँ" के नाम से जाना जाता है।
उत्तरी अफ़्रीका मोर्चा
पाँच उत्तरी अफ्रीकी देश (मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को) यूरोपीय शक्तियों के अधीन औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक थे। सितंबर 1940 में, मुसोलिनी ने ब्रिटिश-नियंत्रित मिस्र पर आक्रमण किया। फरवरी 1941 में, ब्रिटेन ने जवाबी कार्रवाई की और न केवल उत्तरी अफ्रीका में 500 मील क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया, बल्कि एक लाख इटालियंस को भी पकड़ लिया। हिटलर ने इटली को मज़बूत करने के लिए जनरल रोमेल की कमान में जर्मन सेना भेजी, जिसने मार्च के अंत में ब्रिटिश सेना को लीबिया की ओर खदेड़ दिया। जून 42 में जनरल रोमेल और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन को रेगिस्तान में धकेल दिया और तबारुक (लीबियाई बंदरगाह) पर क़ब्ज़ा कर लिया।
बाल्कन क्षेत्र
उत्तरी अफ्रीका में जनरल रोमेल के नेतृत्व में जर्मन अभियान चल रहा था और इस बीच अन्य जर्मन जनरल बाल्कन में लामबंद हो गए। दक्षिणपूर्वी यूरोप में बाल्कन देशों पर कब्ज़ा करना हिटलर की रूस पर आक्रमण की योजना का हिस्सा था। 1941 की शुरुआत में, हिटलर ने बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी को अपने एक्सिस गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर किया और अप्रैल 1941 में यूगोस्लाविया और ग्रीस के ब्रिटिश समर्थक देशों पर आक्रमण किया और क़ब्ज़ा कर लिया।
रूस पर आक्रमण
बाल्कन पर कब्ज़ा करने के बाद, हिटलर ने 22 जून, 1941 को "ऑपरेशन बारब्रोसा" कोड नाम के तहत रूस पर आक्रमण शुरू किया। नवंबर की शुरुआत में जर्मन सेना ने बाल्टिक राज्यों और यूक्रेन को रौंदने के बाद लेनिनग्राद को घेर लिया और उसे शेष रूस से काट दिया। लंबी घेराबंदी के परिणामस्वरूप, शहर के लगभग दस लाख नागरिक भूख और ठंड से मर गए, लेकिन शहर पराजित नहीं हुआ।
अक्टूबर 1941 में, जर्मन सेना ने रूसी राजधानी "मॉस्को" पर हमला किया, लेकिन दिसंबर में, भीषण सर्दी के कारण, आगे बढ़ना असंभव था, इसलिए वे मौसम बदलने की प्रतीक्षा में मॉस्को से 125 मील पश्चिम में छिप गए। चर्चिल के इस डर को देखते हुए कि रूस पर कब्ज़ा करने से जर्मनी यूरोप में एक प्रमुख शक्ति बन जाएगा और ब्रिटेन के लिए और अधिक खतरनाक हो जाएगा, ब्रिटेन ने रूस का समर्थन करने का फ़ैसला किया। उसी समय, चीन भी मित्र राष्ट्रों का सहयोगी बन गया।
युद्ध और अमेरिका
हालाँकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में युद्ध में शामिल न होने की नीति बनाए रखी, मार्च 1941 में ब्रिटेन को हथियार बेचने और उसके जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करने के फ़ैसले से अटलांटिक में जर्मनी के साथ तनाव के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका हिटलर के ख़िलाफ़ एक अनौपचारिक "नौसेना युद्ध" में शामिल हो गया। लेकिन युद्ध में अमेरिका की औपचारिक भागीदारी जापान के प्रशांत क्षेत्र पर आक्रमण से हुई।
जापान का प्रशांत अभियान
जर्मनी की तरह जापान की महत्वाकांक्षाएँ भी विस्तारवादी थीं। ग्रेटर ईस्ट एशिया ने "कॉमन प्रॉस्पेरिटी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस" (पैन-एशिया) की स्थापना के नाम पर चीन में पश्चिमी प्रभाव के प्रभुत्व को समाप्त करने का मिशन अपनाया।
1931 में पूर्वोत्तर चीन में "मंचूरिया" पर क़ब्ज़े के बाद, मध्य चीन एक लंबे युद्ध में फंस गया। इसलिए, अपनी अर्थव्यवस्था पर दबाव के कारण, उन्होंने संसाधनों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिमी उपनिवेशों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जुलाई 1941 में जापान के फ्रांसीसी इंडोचाइना (वियतनामी, लाओस और कंबोडिया) पर क़ब्ज़े के साथ, अमेरिका ने अमेरिका में जापान की संपत्ति ज़ब्त कर ली और फिलीपींस और गाम्बिया में अपने उपनिवेशों को तेल की आपूर्ति बंद कर दी। लेकिन जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ-साथ प्रशांत महासागर में अमेरिकी ठिकानों पर क़ब्ज़ा करने की योजना जारी रखी। इस संबंध में, 7 दिसंबर, 1941 को हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर के अमेरिकी बंदरगाह में बेड़े पर अचानक हमला करके में 8 युद्धपोतों, सहित 188 विमानों को तबाह कर दिया और 2300 चालक दल के सदस्यों की हत्या कर दी। जवाब में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से जापान और उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
"पर्ल हार्बर" पर हमले के बाद, जापान ने ब्रिटिश उपनिवेश "हांगकांग" और अमेरिका-नियंत्रित "गाम" और "वेक आइलैंड" पर क़ब्ज़ा करने के बाद अप्रैल 42 में फिलीपींस पर भी क़ब्ज़ा कर लिया। जहां से उसने भारत पर हमले की योजना के तहत दक्षिण भारत के तटीय इलाक़ों पर बमबारी की। दूसरी ओर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने का अभियान शुरू कर दिया।
मित्र राष्ट्रों के वर्चस्व की शुरुआत
1942 के वसंत तक, धुरी शक्तियां तीन प्रमुख युद्ध मोर्चों (प्रशांत, रूस, और उत्तरी अफ्रीका) पर नियंत्रण कर चुकी थीं। जापान ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया (इंडोचीन, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस) और कई प्रशांत द्वीपों (न्यू गिनी और सोलोमन) के तटों पर क़ब्ज़ा कर लिया था। जर्मनी ने मास्को तक यूरोप पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। उत्तरी अफ्रीकी मोर्चे पर, धुरी जर्मनी की स्थिति मित्र राष्ट्रों की तुलना में अधिक मज़बूत थी। हालाँकि, 1942 के मध्य से मित्र राष्ट्रों की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। तीन निर्णायक लड़ाइयों (मेडवे, स्टेलिनग्राद और अलामीन) ने युद्ध का रुख मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मोड़ दिया।
मेडवे की लड़ाई
मई 1942 में, कोरल सागर की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों को भारी नुक़सान झेलने के बाद जापानियों की दक्षिण की ओर प्रगति रुक गई। 4 जून को जापानियों ने हवाई द्वीप से 1,500 मील पश्चिम में मेडवे द्वीप पर एक अमेरिकी हवाई क्षेत्र पर हमला किया। लेकिन अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में उसके 332 विमान, 4 विमान वाहक और एक सहायता जहाज़ को नष्ट कर दिया, जिससे जापान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मेडवे की लड़ाई में सफलता ने प्रशांत क्षेत्र में युद्ध का रुख मित्र राष्ट्रों के पक्ष में मोड़ दिया। उसके बाद, उन्होंने आक्रामक नीति अपनाई और अगस्त 1942 में "सोलोमन द्वीप" में जापानी हवाई क्षेत्र पर सेना उतार दी। छह महीने की गहन लड़ाई के बाद, उन्होंने फरवरी 1943 में जापानियों से द्वीप पर क़ब्ज़ा कर लिया।
उत्तरी अफ़्रीकी मोर्चा
जून 1942 से जर्मनों ने लीबिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह "टोब्रुक" पर कब्ज़ा कर लिया। जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी सेना की कमान संभालने के लिए जनरल "मोंटगोमरी" को भेजा। उस समय, जर्मन "अलेक्जेंड्रिया" (इस्तांबुल) के पश्चिम में मिस्र के गांव "अलामिन" की ओर आगे बढ़े। 23 अक्टूबर की रात को 1000 ब्रिटिश सैनिकों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। 4 नवंबर को जनरल रोमेल की जर्मन सेना पश्चिम की ओर पीछे हट गई।
8 नवंबर को, अमेरिकी जनरल आयरन हॉवर की कमान के तहत 100,000 सैनिक मोरक्को और अल्जीरिया में उतरे। मई 1943 में, जनरल मोंटगोमरी और जनरल आइजन हॉवर की सेनाओं ने रोमन जनरल रोमेल की "अफ्रीका कोर" को हराया और उत्तरी अफ्रीका में युद्ध जीत लिया।
स्टेलिनग्राद की लड़ाई
दिसंबर 1941 में जर्मन सेना मास्को के बाहरी इलाक़े में रुकी। मौसम बदलने के बाद अगले साल यह फिर सक्रिय हो गया। उसी वर्ष, हिटलर ने दक्षिणी रूस के एक औद्योगिक शहर स्टेलिनग्राद पर हमला करने के लिए छठी सेना भेजी। 23 अगस्त 42 को स्टेलिनग्राद की लड़ाई शुरू हुई। जर्मनों ने भारी बमबारी करके शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया और शहर के 90 प्रतिशत हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया। लेकिन 19 नवंबर को, रूसी सेना और नागरिकों ने गंभीरता से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 2 फ़रवरी 1943 को 330,000 की जर्मन सेना में से बचे हुए 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार ने जर्मनों को हमला करने के बजाय बचाव करने के लिए मजबूर कर दिया। रूसियों ने उन्हें बाल्कन (हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया) से बाहर धकेलते हुए पश्चिम की ओर धकेलना शुरू कर दिया।
इटली पर आक्रमण
रूसी मोर्चे पर जर्मनों के पीछे हटने के साथ, मित्र राष्ट्रों ने 10 जुलाई 1943 को सिसिली पर आक्रमण किया और एक महीने के भीतर उसे जर्मनों और इटालियंस से ख़ाली करा लिया। इस हार के कारण मुसोलिनी को गद्दी से उतार दिया गया और गिरफ़्तार कर लिया गया। नई सरकार के तहत, इटली ने 3 सितंबर को आत्मसमर्पण कर दिया, हालांकि जर्मनों ने फिर उत्तरी इटली पर नियंत्रण हासिल कर लिया और मुसोलिनी को सत्ता सौंप दी। लेकिन आखिरकार, जब जर्मन उत्तर की ओर पीछे हट गए, तो मित्र राष्ट्रों ने 4 जून, 1944 को रोम में प्रवेश किया, लेकिन मई 1945 में जर्मन आत्मसमर्पण तक इटली में लड़ाई जारी रही।
फ़्रांस की पुनर्प्राप्ति
6 जून, 1944 को अमेरिकी जनरल आइजनहावर की कमान के तहत मित्र देशों की सेना ने नॉर्मंडी के समुद्र तटों से फ्रांस पर आक्रमण शुरू किया। पहले दिन की इस भीषण लड़ाई में मित्र सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। जिसके कारण इसे डी-डे कहा जाने लगा। हालाँकि, मित्र राष्ट्रों ने समुद्र तट पर नियंत्रण बरकरार रखा। कुछ सप्ताह बाद 10 लाख की अतिरिक्त सेना के आने से मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ गई। 25 जुलाई को जर्मनी ने रक्षात्मक नाकाबंदी तोड़ दी। अगले महीने अगस्त में मित्र राष्ट्रों ने पेरिस में प्रवेश किया। और सितंबर तक फ्रांस, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग को जर्मन क़ब्ज़े से छुड़ा लिया गया।
उसके बाद मित्र राष्ट्रों का अगला लक्ष्य जर्मनी था। मित्र सेनाएँ पश्चिम से और रूसी सेना पूर्व से आगे बढ़ीं। इस स्थिति में हिटलर ने पश्चिमी सीमा पर जवाबी हमले का आदेश दिया। 16 दिसंबर को जर्मन टैंकों ने मित्र राष्ट्रों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालाँकि, इस टैंक युद्ध (जिसे "बैटल ऑफ़ द बल्ज" (The Battle of the Bulge) के रूप में जाना जाता है) में, जर्मन अंततः पीछे हट गए। बल्ज की लड़ाई के बाद, जर्मनी की हार निश्चित लग रही थी। मार्च 1945 में, मित्र राष्ट्रों ने राइन नदी को पार किया और जर्मनी में प्रवेश किया। 25 अप्रैल तक, बर्लिन शहर 3 मिलियन मित्र देश के सैनिकों और 6 मिलियन रूसी सैनिकों से घिरा हुआ था। 30 अप्रैल को, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। 7 मई, 1945 को जर्मन सेना के आत्मसमर्पण से यूरोपीय मोर्चे पर लगभग 6 वर्षों से चल रहा युद्ध समाप्त हो गया।
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिति
मार्च 1944 के मध्य में मित्र राष्ट्रों (जिनकी जमीनी सेना में ब्रिटेन के अलावा ब्रिटिश भारत और दक्षिण अफ्रीका के सैनिक भी शामिल थे) ने बर्मा पर कब्ज़ा करने के लिए जापान के ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू किया, जिस पर 22 मार्च को जापानी सेनाओं ने भारत के उत्तरपूर्वी सीमावर्ती राज्य "मणिपुर" में स्थित "इम्फाल" मैदान में ब्रिटिश सेना को घेर लिया। यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता "सुभाष चंद बोस" द्वारा बनाई गई "आज़ाद हिन्द फ़ौज" जापान की समर्थक थी। हालाँकि, कई महीनों तक यहाँ लड़ने में सफल नहीं होने के कारण जापानी जुलाई में बर्मा लौट आए। वर्ष के अंत तक, क्षेत्र में मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफी स्थिर हो गई और वे अगले वर्ष (1945) वे बर्मा को जापानियों से मुक्त कराने में सफल रहे।
प्रशांत मोर्चे की अंतिम लड़ाई
अक्टूबर 1944 से, जापान के विरुद्ध मित्र देशों की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई थी। फिलीपींस में “लेटे” (Leyte) द्वीप की लड़ाई में, जापानी नौसेना की युद्ध शक्ति नष्ट हो गई थी, और उसके पास केवल ज़मीनी सैनिक और आत्मघाती पायलट रह गए थे। मार्च 1945 में, भारी लड़ाई और भारी हताहतों के बाद, मित्र राष्ट्रों ने टोक्यो से 750 मील दूर इवो जिमा द्वीप पर क़ब्ज़ा कर लिया। अप्रैल में, जापानियों ने दक्षिणी जापान से 350 मील दूर ओकिनावा द्वीप पर हमला किया। लेकिन 21 जून को इस भीषणतम भूमि युद्ध में वे हार गये। इस युद्ध में एक लाख जापानी और 12 हज़ार अमेरिकी सैनिक मारे गये।इसके बाद मित्र राष्ट्रों की अगली मंज़िल जापान थी। जब जापानियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी के बावजूद हथियार डालने से इनकार किया, तो उन्होंने 6 और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। अंततः 2 सितम्बर को जापान के आत्मसमर्पण करने से यह लम्बा और भयावह युद्ध समाप्त हो गया।
परिणाम और प्रभाव
हताहत: इतिहास के इस सबसे विनाशकारी युद्ध में कम से कम 73 मिलियन लोग मारे गए थे। इस युद्ध का अधिक बर्बर और क्रूर पहलू यह है कि इसमें सैनिकों और लड़ाकों की तुलना में ग़ैर-लड़ाके नागरिक अधिक मारे गए थे। एक सावधानीपूर्वक लिए गए अनुमान के अनुसार, मारे गए सैनिकों की संख्या 24 मिलियन थी, जबकि निर्दोष नागरिकों की संख्या लगभग 50 मिलियन (49 मिलियन) थी। मरने वाले सैनिक हों या ग़ैर-सैनिक थे, सब के सब इंसान थे। स्रष्टा ने उन्हें जीने का अधिकार दिया था, मगर वे अपने ही जैसे इंसानों की सत्ता की भूख की भेंट चढ़ गए।
भौतिक और आर्थिक प्रभाव: युद्ध ने यूरोप के लगभग हर शहर को बर्बाद कर दिया। संचार और परिवहन प्रणालियाँ नष्ट हो गईं। उद्योग, कृषि और व्यापार क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे यूरोप में दीर्घकालिक बेरोजगारी पैदा हो गई और लम्बे समय तक लोगों को भूख और अकाल का सामना करना पड़ा।जापान के दो शहरों का तो अस्तित्व ही मिट गया। इंसानों के हाथों हुए विनाश के 75 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वे शहर जो कभी बेहद विकसित थे, आज निशाने इबरत बने हुए हैं। उन बमों का असर यह है कि आज भी वह जगह इंसानों के बसने के योग्य नहीं है।
सामाजिक प्रभाव: युद्ध का एक परिणाम यूरोप में बड़े पैमाने पर जनसंख्या विस्थापन था। जर्मनों पर रूसियों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किए गए। जर्मनों को पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया और हंगरी से निष्कासित कर दिया गया। 1945/46 के बीच, 12 लाख जर्मनों को पश्चिम जर्मनी में धकेल दिया गया। जर्मनों के अलावा, कई अन्य लोग (सर्ब, यहूदी, मुस्लिम, क्रोएट, पोल्स, यूक्रेनियन, आदि) के कैदियों और निवासियों को भी विरोधी दलों द्वारा गंभीर उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होना पड़ा। अपार हत्याएँ, बेदख़ली, बेरोज़गारी। अकाल, ग़रीबी और बीमारियों के कारण लाखों लोग गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित हुए।
भू-राजनीतिक परिणाम: कुछ जर्मन प्रांतों को पोलैंड और रूस ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया, जबकि शेष जर्मनी को दो भागों (पश्चिम और पूर्व) में विभाजित कर दिया गया। दो पोलिश प्रांत, उत्तरपूर्वी रोमानिया। पूर्वी फ़िनलैंड के कुछ हिस्से और तीन बाल्टिक राज्यों को रूस ने अपने अधीन कर लिया। जापान को अमेरिकी प्रशासन के अधीन लाया गया। कोरिया को भी दो भागों (उत्तर और दक्षिण) में बाँट दिया गया।
दो महाशक्तियाँ: यूरोप की पारंपरिक शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) के बजाय अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरे। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद के कारण यूरोप क्रमशः अमेरिका और रूस के नेतृत्व में "पूंजीवादी लोकतंत्र" (पश्चिमी यूरोप) और "कम्युनिस्ट ब्लॉक" (पूर्वी यूरोप) में विभाजित हो गया। अमेरिका और उसके समर्थक देशों (पूंजीवादी लोकतंत्र) और रूस और उसके समर्थक देशों (कम्युनिस्ट ब्लॉक) के बीच वैचारिक संघर्ष केवल विचारधारा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने शीत युद्ध का रूप ले लिया। "शीत युद्ध" के विभिन्न आयाम अगले कुछ दशकों तक वैश्विक स्तर पर बने रहे। उग्र राष्ट्रवाद के हानिकारक प्रभावों और साम्यवाद के ख़तरे को देखते हुए पश्चिमी यूरोप के देश सहयोग, एकजुट होने और मेल-मिलाप के लिए इच्छुक हो गये।
संयुक्तराष्ट्र का गठन: संयुक्तराष्ट्र संगठन का गठन भविष्य में युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। इसका विवरण उनके क्रम के अनुसार आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत किया जाएगा।
उपनिवेशों का बिखराव: यूरोप का विदेशी उपनिवेशों का साम्राज्य ढहने लगा। भारत, फिलीपींस, बर्मा (म्यांमार), श्रीलंका,। इन्डोचीन, इंडोनेशिया शीघ्र ही स्वतंत्र हो गए। राष्ट्र संघ के आदेश के तहत, ब्रिटेन और फ्रांस की देखरेख में मध्य पूर्व के अरब देश (फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक़) भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए।
(संयुक्तराष्ट्र ने फ़िलिस्तीन के एक भाग को अलग कर इसराईल राज्य की स्थापना की) इस पर भी अगले पृष्ठों में विस्तार से चर्चा की जायेगी।
1950/1960 के दशक तक, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के शेष नव-औपनिवेशिक देशों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।
बौद्धिक प्रभाव: युद्ध की भीषण क्रूरता और मानवीय अत्याचारों ने यूरोपीय लोगों के तर्क में विश्वास को हिला दिया और उन्हें बौद्धिक अराजकता से पीड़ित कर दिया, जिसने विभिन्न मामलों में दिमाग और विचार के कोणों को बदल दिया।
अगर हम युद्ध के पूरे परिदृश्य और क्रमशः देशों की भागीदारी की जांच करें तो यह स्पष्ट होता है कि यह युद्ध शुरू से अंत तक सत्ता की लालसा, सत्ता छिन जाने के डर, दूसरों को सत्ता से रोकने, अंधे प्रतिशोध और इसी जैसे नकारात्मक और मानव विरोधी उद्देश्यों के लिए लड़ा गया था। सत्ता की लालसा में एक पक्ष ने विश्व को अपने अधीन करने का शैतानी इरादा बना लिया, कुछ देश उसमें हिस्सेदारी पाने के प्रलोभन में उसके साथ हो गये और कुछ अन्य देश उसके विरुद्ध संगठित होने लगे। इस प्रकार युद्ध के विरुद्ध युद्ध, अत्याचार के विरुद्ध अत्याचार तथा हिंसा के विरुद्ध हिंसा का एक लम्बा सिलसिला चला। पहले धुरी शक्तियों ने हिंसा और अत्याचार के माध्यम से एक-एक करके कई देशों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया। लाखों इन्सानों की जान लेकर और लाखों को बेघर करके कई देशों को अपनी सत्ता के अधीन कर लिया। फिर मित्र देशों की शक्तियों ने इसी रास्ते से गुज़र कर लाखों लोगों की करके और लाखों को विस्थापित कर के उन देशों को पुनः स्वतंत्र कराया। पहली ताक़त ने भी अपनी सीमा का उल्लंघन किया और दूसरी ने भी। पहली शक्ति की कार्रवाइयों का शिकार भी मानवता हुई और दूसरी शक्ति के प्रयासों के अधीन भी मानवता ही आई। इतना सब कुछ होने के बावजूद, दुनिया में शक्ति के केंद्र बदल गए, लेकिन युद्ध का कारण वहीं रहा, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रयास किया ही नहीं गया था।
शीत युद्ध
विकसित हैं हम, हमारी प्रवृति में है युद्ध
सशस्त्र युद्ध निषिद्ध है तो शीत युद्ध करें
डी. एफ. फ्लेमिंग के अनुसार, “शीत युद्ध शक्ति-संघर्ष की राजनीति का मिला-जुला परिणाम है। दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। विरोधी चिन्तन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है।"
वस्तुतः शीत युद्ध विश्व को दो विरोधी विचारधाराओं,दो पद्धतियों,दो गुटों तथा दो पृथक् चिन्तन सारणियों से उत्पन्न तनावों का परिणाम था। ये विरोधी विचारधाराएँ पूंजीवादी तथा साम्यवादी हैं। इनमें से एक जनतन्त्र का सहारा लेती है, तो दूसरी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का। ये गुट क्रमशः नाटो तथा वारसा पैक्ट के समर्थक थे। इनका संचालन अमेरिका तथा सोवियत रूस द्वारा किया जाता था। वस्तुत: शीत युद्ध को हम युद्ध न कहकर युद्ध का वातावरण कह सकते हैं । इसका मुख्य साधन उग्र या नरम सभी प्रकार के कूटनीतिक दाँवपेंच खेलना है तथा दूसरे पक्ष को कमज़ोर बनाने का प्रयास करना है।
द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत संघ और अमेरिका स्वार्थवश एक हो गए थे, परन्तु बाद में दोनों के मध्य मतभेद गम्भीर रूप धारण करने लगे। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और अपने-अपने स्वार्थों के कारण मतभेदों ने विश्व में एक गहरा तनाव उत्पन्न कर दिया। इस तनाव व युद्ध की स्थिति को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। यह एक प्रकार का वाक युद्ध है।जिसे पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों द्वारा लड़ा जाता है। यह एक प्रचारात्मक युद्ध है, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के ख़िलाफ़ घृणित प्रचार का सहारा लेती है। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी है।
शीत युद्ध अस्त्र-शस्त्रों से न लडा जाकर अन्य साधनों से लड़ा जाता है । इस युद्ध में किसी भी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती,परन्तु इस युद्ध के द्वारा भयानक सर्वनाश और लाखों हत्याओं की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।
नव-स्वतन्त्र राष्ट्र अथवा अन्य दुर्बल राष्ट्र इन दोनों में से किसी-न-किसी एक को अपना नेता मान रहे थे और उन्हीं के राजनीतिक निर्देशों के अनुसार अपने विकास कार्या में संलग्न थे। ये दोनों महाशक्तियाँ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इतनी अधिक शक्तिशाली हो गई कि एक या कई राष्ट्र भी मिलकर इनका सामना नहीं कर सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों शक्ति गट अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि करते रहे। इससे मतभेद, तनाव और बैर-विरोध की वृद्धि हुई।
शीत युद्ध का उद्देश्य
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता थी। आपसी झगड़े न हों और अगर हों तो उन्हें शान्तिपूर्वक निपटाया जाए, इस दृष्टि से संयुक्तराष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इससे सम्पूर्ण विश्व में एक आशा की लहर दौड़ गई। किन्तु आशा की यह मधुर कामना बहुत दिनों तक नहीं टिकी और युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों के दो गुट बन गए । उनमें परस्पर द्वेष, वैमनस्य एवं अपने प्रभाव-वर्धन के लिए होड़ लग गई। इनमें एक गुट का अगुआ था अमेरिका और दूसरे गुट का नेता बना सोवियत रूस।
वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ एक-दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि दोनों का जीवन-दर्शन अलग-अलग था। अमेरिका लोकतन्त्र और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद को। किन्तु परिस्थितिवश युद्ध में दोनों को फासिस्टवाद के विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध करना पड़ा, अन्यथा सम्पूर्ण यूरोप ही नहीं सम्पूर्ण विश्व फासीवाद की चपेट में आ जाता। युद्धोन्मादी जर्मनी और इटली फासिस्ट ताकतों के पतन के बाद ही पश्चिमी शक्तियों और रूस की अस्थायी मैत्री में दरार पड़नी प्रारम्भ हो गई। विश्व समस्याओं और विजित राष्ट्रों को लेकर उनमें गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गए। दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर कीचड़ उछालने लगे। फलतः वैमनस्य बढ़ता गया और बैर-विरोध इतना बढ़ गया कि विश्व दो गुटों में बँट गया। दोनों गुटों के पृथक्-पृथक् चौधरी क्रमश: अमेरिका तथा सोवियत संघ हुए। इस प्रकार शीत युद्ध का उदय हुआ। पारस्परिक अविश्वास के वातावरण में दोनों चौधरियों ने अपने-अपने क्षेत्रीय सैनिक संगठन बनाए और एक-दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सैनिक मोर्चे पर पराजित करने का प्रयास किया। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के उपरान्त ही दो महाशक्तियों में शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया।
शीत युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भय,घृणा, परस्पर अविश्वास के वातावरण को न केवल जन्म दिया,वरन् इसे निरन्तर बनाए रखा। यहाँ तक कि देतान्त के युग में भी यह मनोवृत्ति बनी रही।
सन् 1945 के बाद द्विध्रुवीकरण की राजनीति शीत युद्ध की प्रमुख देन है । विश्व की सभी समस्याओं को दो गुटों के आधार पर हल करने का असफल प्रयास किया गया, जिससे समस्याओं ने गम्भीर रूप धारण किया; जैसे-कोरिया विवाद, बर्लिन प्रश्न, वियतनाम समस्या, अरब-इसराईल संघर्ष आदि।
शीत युद्ध ने सैनिक मनोवत्ति को पुख्ता किया, जिसके फलस्वरूप नाटो,सेण्टो,सीटो तथा वारसा सन्धि जैसे सैनिक गठबन्धनों का जन्म हुआ। इससे न केवल शीत युद्ध में उग्रता आई।वरन निःशस्त्रीकरण समस्या और भी अधिक जटिल हो गई।
शीत युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्तराष्ट्र को पंगु बनाया है। शीत युद्ध के कारण यह संस्था महाशक्तियों के हितों की पोषक बनकर रह गई तथा यह अपने आदशों एवं लक्ष्यों से भटक गई। परस्पर मनोमालिन्यता के कारण वीटो शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग हुआ। फलतः चार्टर में उपयुक्त संशोधन भी नहीं हो सके।
शीत युद्ध के वातावरण ने महाशक्तियों को आणविक शस्त्रों की होड़ में लगा दिया, जिससे विश्व के देशों को आण्विक आतंक मानसिक रूप से परेशान करने लगा। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई।
शीत युद्ध के फलस्वरूप विश्व की राजनीति दो भीमाकार देशों के मध्य केन्द्रित हो गई तथा मानव-कल्याण से सम्बन्धित कई कार्य ठप्प हो गए। यह शीत युद्ध का ही प्रभाव था कि अमेरिका यूनेस्को' से अलग हो गया।
शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी प्रभावित किया है; जैसे
(i) शीत युद्ध के प्रभाव के कारण ही विश्व की राजनीति में शक्ति सन्तुलन स्थापित हुआ।
(ii) इससे राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ।
(ii) शीत युद्ध के कारण औद्योगिक, तकनीकी, आणविक आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई।
(iv) शीत युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त हुई।
शीत युद्ध की समाप्ति और बदलता राजनीतिक परिदृश्य
सन् 1990 में सोवियत संघ, जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, उसके विखर जाने के बाद विश्व की राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो गया है। अब एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ही रह गया है। अतः अब शीत युद्ध के दिन समाप्त हो गए हैं। रूस ने अमेरिका के साथ सामरिक क्षमता की समदक्षता का दावा पूरी तरह छोड़ दिया है। विनाशकारी अस्त्रों को सीमित करने के मामले में दोनों देशों के बीच बार-बार जो गतिरोध पैदा हो रहा था,उसका कारण यही था कि हथियारों को कम करने की इच्छा के बावजूद दोनों में से कोई यह नहीं चाहता था कि उसकी स्थिति दूसरे से कमज़ोर हो । सोवियत संघ के टूटने के बाद उसके उत्तराधिकारी रूस ने पूरी तरह से अमेरिका के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व की सर्वोच्च शक्ति बन गया है। किसी प्रबल प्रतिरोध के न होने पर कभी स्वतन्त्र समझे जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन-संयुक्तराष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि आज अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। विश्व व्यापार संगठन तथा
अंकटाड जैसे संगठन भी अमेरिकी नीतियों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। विश्व स्तर पर जो भी आर्थिक नीतियाँ निर्धारित हो रही हैं,उन पर अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह अमेरिका की सर्वोच्च शक्ति का ही परिणाम है कि वह अपने सुपर-301 कानून के तहत किसी भी देश को लेकर उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की धमकी दे रहा है। अगर विश्व की राजनीति पर दृष्टिपात करें, तो यही प्रतीत होता है कि आज विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह स्थापित हो गया है। रूस तो पूरी तरह से अमेरिका के सामने आत्म-समर्पण कर ही चुका है और अमेरिका ने भी उसे अपना सबसे प्रिय देश माना है। इसके साथ ही अमेरिका समस्त विश्व पर अपनी सैनिक पकड़ मज़बूत करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रशान्त महासागर, अटलाण्टिक महासागर व फारस की खाड़ी में ही नहीं अरब सागर व हिन्द महासागर में भी उसने अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का निश्चय कर लिया है।
क्रूरता और अन्याय का एक स्थायी अध्याय: फ़िलिस्तीन पर ज़ायोनी क़ब्ज़ा
फ़िलिस्तीन का मुद्दा सदियों पुराना है, लेकिन इस अध्याय में हम उस्मानी ख़िलाफ़त के पतन के बाद की स्थिति की समीक्षा करेंगे। 761 वर्षों तक मुसलमानों के शासन के बाद फ़िलिस्तीन पर 1917 ई. में ब्रिटेन ने क़ब्ज़ा कर लिया। उससे पहले नाज़ी जर्मनी में यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों के कारण फ़िलिस्तीन में यहूदियों का प्रवास शुरू हो गया था। 1896 में एक यहूदी पत्रकार "थियोडोर हर्टज़ल" ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने यहूदियों के लिए एक स्थायी राज्य बनाने का आह्वान किया था और इसके लिए उन्होंने दो स्थानों ‘फ़िलिस्तीन’ या ‘अर्जेंटीना’ की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इनमें से किसी एक को यहूदी राज्य बनाया जाए, जहां सारे यहूदी इकट्ठा हो जाएं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई यहूदी सम्मेलन आयोजित किए गए और धन एकत्र किया गया। फिर फ़िलिस्तीन को वास्तव में एक यहूदी राज्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यहूदियों का प्रवास शुरू हुआ। 1900 में, फ़िलिस्तीन में यहूदी आबादी पांच प्रतिशत के करीब थी, जबकि मुस्लिम 86 प्रतिशत और ईसाई 14 प्रतिशत थे। बड़ी संख्या में यहूदियों के प्रवास से अरबों में चिंता और ग़ुस्से की लहर पैदा होना स्वभाविक था। 1920, 1921, 1929 और 1936 में यहूदियों के प्रवास और इस क्षेत्र में उनके आगमन के ख़िलाफ़ अरबों द्वारा हिंसक प्रदर्शन भी हुए, लेकिन आगमन जारी रहा। 1917 में अंग्रेजों के क़ब्ज़े में आ जाने के बाद और बड़ी संख्या में यहूदियों के प्रवास के बावजूद, 1923 तक फ़िलिस्तीन में केवल 3% भूमि पर यहूदियों का स्वामित्व था और 97% भूमि पर अरबों का स्वामित्व था।
दूसरी ओर, ब्रिटेन को भी इस का बहुत डर था कि यहूदी बड़ी संख्या में ब्रिटेन की ओर रुख न कर लें और फिर उनकी दुष्टता के कारण ब्रिटेन की ईसाई जनता का जीवन दूभर न हो जाए। इसलिए उसने फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के लिए एक योजना प्रस्तुत की और यहूदियों को इसके लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।
2 नवंबर, 1917 को ब्रिटिश राजनेता आर्थर जेम्स बालफोर ने ज़ायोनी यहूदियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि वे फ़िलिस्तीन की भूमि में यहूदी राज्य की स्थापना के लिए पूर्ण और व्यावहारिक समर्थन प्रदान करेंगे, और पत्र में यह भी कहा कि 31 अक्टूबर, 1917 को ब्रिटिश कैबिनेट की एक गुप्त बैठक में इस समझौते की पुष्टि की जा चुकी है। पत्र के शब्द थे:
“प्रिय रोथ्शील्ड!
ब्रिटेन के सम्राट की ओर से आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निम्नलिखित घोषणा ज़ायोनी यहूदी की आशाओं के प्रति हमारी सहानुभूति की अभिव्यक्ति है, और हमारे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। ब्रिटेन की सरकार फ़िलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के पक्ष में है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेगी। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि फ़िलिस्तीन की मौजूदा ग़ैर-यहूदी आबादी (मुस्लिम और ईसाई) के नागरिक और धार्मिक अधिकारों या अन्य देशों में यहूदियों की राजनीतिक स्थिति को नुक़सान न पहुंचे।
मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर इस घोषणा को ज़ायोनी संघ के संज्ञान में लाया जाए।" (विकिपीडिया: बाल्फोर घोषणा)
बाल्फोर के इस पत्र को "बाल्फोर घोषणा" के नाम से जाना जाता है और इसी घोषणा के तहत इसराईल की स्थापना हुई। इसलिए 1947 में संयुक्तराष्ट्र महासभा ने फ़िलिस्तीन का विभाजन कर एक इसराईली राज्य की स्थापना की घोषणा की और 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा लीं और 14 मई 1948 को इसराईल की स्वतंत्र सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। फ़िलिस्तीन का अत्यंत अत्याचारपूर्ण विभाजन करके, मूल प्राचीन निवासियों को केवल 45 प्रतिशत भाग दिया गया और शेष 55 प्रतिशत भाग यहूदियों को दे दिया गया। जबकि उस समय फ़िलिस्तीन में केवल 31 प्रतिशत यहूदी थे और वे केवल 7 प्रतिशत भूमि के मालिक थे।
इसके बाद संघर्षों का सिलसिला जारी रहा और हर संघर्ष का नतीजा यह निकला कि यहूदियों ने और अधिक क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया और उन्हें अपने अवैध राज्य में शामिल कर लिया। 1948 में इसराईली राज्य की स्थापना के तुरंत बाद, जब ब्रिटेन ने अपनी सेना हटा ली, तो यहूदियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच एक स्थाई टकराव शुरू हो गया, जिसके बाद यहूदियों ने अपने सहयोगियों और समर्थकों की मदद से फ़िलिस्तीन के 78 प्रतिशत हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया।
1948 में, इसराईल ने यरूशलेम के पश्चिमी आधे हिस्से पर आक्रमण किया और क़ब्ज़ा कर लिया, जबकि शेष आधा, जिसमें अल-अक्सा मस्जिद भी शामिल थी, जॉर्डन के नियंत्रण में रहा। फिर कुछ साल बाद, 1967 में, इसराईल ने पड़ोसी देशों पर हमला किया और उन क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लिया, जिन्हें संयुक्तराष्ट्र ने अवैध घोषित कर दिया था, इसलिए उन क्षेत्रों को "अधिकृत क्षेत्र" कहा गया।
इस तथ्य के बावजूद कि संयुक्तराष्ट्र द्वारा उन कब्ज़ों को अवैध कहा गया था, इसराईल ने उन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों का निर्माण जारी रखा। इसराईल के निमंत्रण पर, यहूदियों ने पलायन करना और यहां बसना जारी रखा।
जिस ग़ज़्ज़ा पर इसराईल इस समय बमबारी कर रहा है और बीमारों, महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष लोगों का नरसंहार कर रहा है, उस ग़ज़्ज़ा पर भी 2005 तक इसराईल ने अवैध रूप से क़ब्ज़ा कर लिया था, लेकिन 2005 में हमास और अन्य फ़िलिस्तीनी समूहों के दबाव में इसराईल ने ग़ज़्ज़ा से अपना क़ब्ज़ा हटा लिया और अपनी कॉलोनियों को बर्खास्त कर उन्हें फ़िलिस्तीनियों को सौंप दिया। लेकिन अब वहां बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध हो रहे हैं और निर्दोष लोग शहीद हो रहे हैं।वहां इतनी बमबारी हुई है कि जो इलाका कभी इमारतों से बसा हुआ था वह अब खंडहर जैसा दिखाई पड़ता है। कहा जा रहा है कि इसराईल ने पहले ही वहां के लोगों की ज़िन्दगी को क़ैद की ज़िन्दगी में बदल दिया है। और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की कोशिशों के बावजूद उसने यहां से नाकाबंदी नहीं हटाई है।
अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इसराईल की मंशा शुरू से ही ख़राब है कि इस पर उसका क़ब्ज़ा है, लेकिन इसराईल की योजना इसे शहीद करके उस जगह पर हैकल सुलैमानी बनाने की है। यहूदियों का दावा है कि यह मस्जिद सुलैमानी हैकल की जगह पर बनाई गई थी, और अल-अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार सुलैमानी हैकल के अवशेषों में से एक है, जहां यहूदी ज़ायरीन दो हज़ार वर्षों से आ कर रोते रहे हैं। इसीलिए इसे “विलाप वाली दीवार” (Wailing Wall) कहा जाता है। हालाँकि, यह दावा पूरी तरह से झूठ है और वे कभी भी साक्षों के आधार पर यह साबित नहीं कर पाए कि हैकल सुलैमानी यहीं बनाया गया था। लेकिन वे इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी यहूदी योजना को लागू करने और अल-अक्सा मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेनिस माइकल रुहान ने अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी थी, जिसके कारण अल-अक्सा मस्जिद तीन घंटे तक जलती रही और ठीक क़िबला की ओर इसके दक्षिण-पूर्व का बड़ा हिस्सा ठह गया। मेहराब में मौजूद मिम्बर, जिसे बैतुल-मकदिस की विजय के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी द्वारा स्थापित किया गया था, भी जला दिया गया। यह वह मिम्बर था जिसे प्रथम क़िबला की आज़ादी के लिए लड़े गए युद्धों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथ रखते थे, ताकि जीत के बाद उसे मस्जिद में स्थापित किया जाए, फिर जीत के बाद उसे मस्जिद में स्थापित किया गया था।
इसराईल जैसा छोटा राज्य अपने आप में इतना शक्तिशाली नहीं है और न ही हो सकता है कि वह फ़िलीस्तीनी लोगों को अपनी मातृभूमि से निकाल सके। दरअसल, इसराईल के पीछे प्रमुख विश्व शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका का हाथ है। फ़िलिस्तीन की समस्या केवल फ़िलिस्तीन की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति ने इसे इस्लाम और ग़ैर-इस्लाम के बीच संघर्ष का क्षेत्र बना दिया है। सभी इस्लाम विरोधी ताकतें इस्लाम बनाम गैर-इस्लाम के नाम पर यहूदी राज्य इसराईल के साथ सहानुभूति रखती हैं और सहयोग करती हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन को मुस्लिम देशों और मुस्लिम शासकों से कोई समर्थन भी नहीं मिलता है। उन्हें अपनी लड़ाई अकेले और साधनहीनता की हालत में लड़नी पड़ रही है। हां दुनिया भर की मुस्लिम जनता की सहानुभूति फ़िलिस्तीन के साथ है।
कुत्सित प्रयासों की असफलता: वियतनाम युद्ध
जिनेवा समझौते पर 70 दिनों तक चली बातचीत के बाद 21 जुलाई, 1954 को हस्ताक्षर किए गए। ये वार्ताएं 1954 में वियतनाम में डिएनबिएनफु की लड़ाई में फ्रांस की निर्णायक हार के बाद शुरू हुई थीं। लड़ाई 13 मार्च से 7 मई तक चली और फ्रांसीसी सेना की हार पर समाप्त हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं था लेकिन फ्रांस को गुप्त व्यावहारिक सहायता प्रदान कर रहा था।
अगस्त 1945 में, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से हार गया, जिसके कारण जापान को इंडोचीन से निष्कासित होना पड़ा और उसके बाद वहों शक्तिशून्यता पैदा हो गई। फ्रांस, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वियतनाम पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा किया हुआ था, ने वियतनाम पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाते हुए, उसने फिर से वियतनाम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया।
सितंबर 1945 में हुची मिन्ह ने एक स्वतंत्र उत्तरी वियतनाम की घोषणा की और अमेरिकी समर्थन हासिल करने के प्रयास में, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के समान अपने देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हुची मिन्ह ने सोचा कि इससे अमेरिकी खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जुलाई 1946 में, हुची मिन्ह ने वियतनाम को सीमित स्वशासन देने के फ्रांसीसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद, हुची मिन्ह समर्थक सेना "वियत मिन्ह" ने फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। मार्च 1947 में, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने कांग्रेस को दिए एक भाषण में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति ऐसे देश की मदद करने की है जिसकी स्थिरता को साम्यवाद से ख़तरा हो। इस नीति को कोट्रूमैन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। फ्रांस लगातार वियतनाम पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। जून 1949 में, उसने वियतनाम के पूर्व सम्राट बाओ दाई को वियतनाम में राज्य के प्रमुख के रूप में स्थापित कर दिया।
अगस्त 1949 में, सोवियत संघ ने कजाकिस्तान के एक सुदूर इलाक़े में अपना पहला परमाणु बम विस्फोट किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शीत युद्ध का तनाव शुरू हो गया। अक्टूबर 1949 में, गृह युद्ध के बाद, चीनी कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की क्रांति की जीत की घोषणा कर दी। जनवरी 1950 में, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत संघ ने औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम को मान्यता दे दी, और दोनों ने वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट प्रतिरोध सेनानियों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। फरवरी 1950 में, सोवियत संघ और नए कम्युनिस्ट चीन की मदद से, वियतनाम में फ्रांसीसी चौकियों के ख़िलाफ़ वियतनामी अभियान तेज़ हो गए। जून 1950 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनाम को साम्यवादी ख़तरा घोषित किया और इसके ख़िलाफ़ फ्रांस को सैन्य सहायता बढ़ा दी।
मार्च-मई 1954 में, डिएनबिएनफु में वियत मिन्ह सेना ने फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। इस हार ने इंडो-चीन में फ्रांसीसी शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। अप्रैल 1954 में एक भाषण में, अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा कि इंडो-चीन में कम्युनिस्टों के हाथों फ्रांसीसी शासन के अंत का दक्षिण पूर्व एशिया में डोमिनोज़ प्रभाव हो सकता है। यह तथाकथित डोमिनो सिद्धांत अगले दशक तक वियतनाम के बारे में अमेरिकी सोच का मार्गदर्शन करता रहा।
जुलाई 1954 में, जिनेवा समझौते ने उत्तर और दक्षिण वियतनाम के विभाजन को औपचारिक रूप दिया। समझौते में यह भी तय हुआ कि वियतनाम को एक लोकतांत्रिक सरकार के तहत एकजुट करने के लिए दो साल के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन ये चुनाव कभी नहीं हुए।
1946 में शुरू हुए आठ लंबे वर्षों के युद्ध के बाद, फ्रांसीसियों को एहसास हुआ कि भारी नुक़सान और अंधकारमय भविष्य को देखते हुए, वे वियत मिन्ह को नहीं हरा सकते। इसके अलावा, फ्रांस में वियतनाम युद्ध के ख़िलाफ़ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी बढ़ गया। इसलिए, फ्रांसीसी शासकों ने बातचीत के माध्यम से वियतनाम में युद्ध को समाप्त करना बेहतर समझा। हालाँकि, उन्होंने सोचा कि उन्हें वियत मिन्ह सेना को युद्ध के मैदान कम से कम एक मोर्चे पर हरा कर बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि जब वे मेज़ पर बैठें, तो एक विजेता की तरह बात कर सकें और अपनी शर्तें रख सकें। इसलिए, जब फ्रांसीसी सेना को एक गुप्त रिपोर्ट मिली कि वियत मिन्ह उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, तो फ्रांसीसी ने इसे अपने लिए एक सैन्य अवसर माना। उन्होंने इसे वियत मिन्ह के नियमित सैनिकों को हराने का एक उत्कृष्ट अवसर के रूप में देखा।
फ्रांसीसी जनरलों ने जल्द ही वहां एक मज़बूत रक्षात्मक स्थिति स्थापित करने के लिए अपनी सेना को डिएनबिएनफु में भेज दिया। वियत मिन्ह सेना भी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। (डिएनबिएनफु लाओस की सीमा के पास, उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई के पश्चिम में एक महत्वपूर्ण शहर है)। इस कारण से, वियत मिन्ह जनरल वु गुयेन गियाप के अनुसार, डिएनबिएनफु दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक निर्णय का मैदान बन गया।
वियतनाम में फ्रांस की हार को औपचारिक रूप से जिनेवा समझौते में मान्यता दी गई थी, और उसी समझौते में वियतनाम को दो अलग-अलग प्रशासन के रूप में स्वीकार किया गया था। एक क्षेत्र उत्तरी वियतनाम था, जो 1945 से वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम पर था और हुची मिन्ह के साथ संबंध के कारण वियतनाम के नियंत्रण में था, और दूसरा दक्षिण वियतनाम था, जहां राजशाही बहाल की गई थी और पश्चिम समर्थक और कम्युनिस्ट विरोधी नेता, न्गोदिन्हदीम की सरकार की स्थापना की गई। यह विभाजन पहले से ही चल रहा था, लेकिन फ्रांस को हार की शर्मिंदगी से बचाने के लिए जिनेवा की संधि में इसे औपचारिक रूप दिया गया। फ़्रांस ने दक्षिण वियतनाम से अपने सैनिकों की क्रमिक वापसी शुरू कर दी। उसके बाद, दक्षिण वियतनाम जल्द ही अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन गया।
जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वियतनाम पर फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त हो गया, लेकिन इसके साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप का इतिहास भी शुरू हो गया और 4 अगस्त, 1964 को टोंकिन की खाड़ी की घटना के बाद वियतनाम में अमेरिकी सेनाओं का सीधा हस्तक्षेप शुरू हो गया। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में 550,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया। अमेरिकी सेना के सीधे हस्तक्षेप के बाद, हुची मिन्ह समर्थक वियत मिन्ह के साथ एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। वियतनाम संकट दो दशकों के बाद 1975 में समाप्त हुआ।
1960 के दशक में जब अमेरिकी सेना दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची, तो हज़ारों साल पुराना वियतनाम देश दो अलग-अलग देशों, साम्यवादी उत्तरी वियतनाम और ग़ैर-साम्यवादी दक्षिणी वियतनाम में विभाजित हो गया था।
जिनेवा समझौते ने लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में युद्धविराम की स्थापना की और वियतनाम में दो 'पुनर्गठन' क्षेत्र, डिमिलिटराइज्ड जोन (डीएमजेड) की स्थापना की। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का विभाजन केवल 1956 तक चलना था, जिसके बाद पूरे देश में एकीकृत सरकार बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय चुनाव होने थे।
वियतनाम अब स्थायी रूप से विभाजित हो गया है, इस चरण में एक भूराजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ा जहां अमेरिकी सेना ने दक्षिण वियतनाम को ग़ैर-साम्यवादी और स्वतंत्र रखने के लिए लड़ने के लिए अशांत क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप किया। सवाल उठता है, यह देखते हुए कि वियतनाम में वास्तविक संघर्ष वियतनाम और फ्रांस के बीच था, इन वार्ताओं में चार प्रमुख शक्तियां क्यों शामिल थीं? 1946 के अंतरिम समझौते की तरह वियतनाम और फ्रांस के बीच ये बातचीत क्यों नहीं हुई?
1953-1954 की अवधि में इंडो-चीन युद्ध वियतनाम और फ्रांस के बीच नहीं लड़ा गया था। युद्ध के लिए पर्याप्त धन और हथियारों के लिए, फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर था, जो कुछ नुक़सान के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी रहा था।
'और अब (अमेरिका) एक मज़बूत साम्राज्यवादी देश था और पूंजीवादी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका की मूल योजना धीरे-धीरे सहायता प्रदान करके वियतनाम में फ्रांस की जगह लेने की थी। इसलिए इंडो-चीन युद्ध के बाद के चरण में, अमेरिका ने फ्रांसीसियों पर अपना दबाव बढ़ाया और उन्हें अपनी योजनाओं पर अमल करने के लिए मजबूर किया।
हालाँकि 1954 में वियतनाम और फ्रांस दोनों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने का इरादा किया था, स्थिति 1945 से 1946 के युद्ध से भिन्न थी क्योंकि अब युद्ध में केवल दो पक्ष शामिल नहीं थे।
'शीत युद्ध की दोनों विश्व शक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, इस स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने जिनेवा सम्मेलन बुलाया और वार्ताकार दलों के रूप में उसमें भाग लिया।
यह दोनों विश्व शक्तियों का हित ही था कि जिनेवा सम्मेलन 8 मई से 21 जुलाई, 1954 तक अर्थात् 75 दिनों तक चला। भाग लेने वाले देशों ने ऐसे रुख अपनाए जो उनके अपने हित में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस पर दबाव डाला और सोवियत संघ ने पश्चिम में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए वियतनाम का इस्तेमाल किया।
वियतनाम अन्य समाजवादी देशों के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन सबसे पहले वह अपने बुनियादी राष्ट्रीय हितों, स्वतंत्रता, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना चाहता था। इसलिए, उसने कड़ी कोशिश की और संयुक्त राज्य अमेरिका की कमज़ोरियों को निशाना बनाया और अंततः 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनाम से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका निस्संदेह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था, और उसका मानना था कि उसकी सेना भी सबसे शक्तिशाली है। लेकिन आठ साल के युद्ध में अनगिनत सैनिकों और विशाल संसाधनों को झोंकने के बाद भी, संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी वियतनामी सेनाओं और उनके गुरिल्ला सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। युद्ध के चरम पर, अमेरिका के पास वियतनाम में पांच लाख से अधिक सैनिक थे। युद्ध की लागत अथाह थी - 2008 में अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में युद्ध की कुल लागत $ 686 बिलियन (आज के डॉलर में $ 950 बिलियन से अधिक) बताई गई थी। लेकिन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में चार गुना से अधिक खर्च किया और जीत हासिल की थी, और कोरिया जैसै दूर देश में जाकर युद्ध लड़ा था, इसलिए अमेरिका के पास आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी।
1968 तक, अमेरिकी सरकार को विश्वास था कि वह इस सुदूर देश में भी युद्ध जीत लेगी। हालाँकि, यह विश्वास जल्द ही समाप्त हो गया। विशेष रूप से, जनवरी 1968 में कम्युनिस्ट हमलों के कारण युद्ध के वित्तपोषण के लिए अमेरिकी कांग्रेस के समर्थन में कमी आई और अंततः 1973 में अमेरिका को वियतनाम से अपने लड़ाकू सैनिकों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अमेरिकी सेना को इस प्रकार के युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। यहां के कुछ हिस्से दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे घने जंगलों में से हैं। अमेरिकी सेना इस माहौल से नहीं निपट सकी, जबकि उत्तरी वियतनामी और वियतनामी कांग्रेस इसके अभ्यस्त थे, हालांकि उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा।
स्थानीय लड़ाकों ने अपनी शर्तों पर युद्ध का समय और स्थान चुना, और लाओस और कंबोडिया में सीमा पार सुरक्षित ठिकानों पर पीछे हटने में सक्षम रहे जहां अमेरिकी सेना द्वारा पीछा करना संभव नहीं था।
इस युद्ध को अक्सर "पहला टेलीविज़न युद्ध" कहा जाता है और इसके मीडिया कवरेज की सीमा अभूतपूर्व थी। 1966 तक, यूएस नेशनल आर्काइव्स ने अनुमान लगाया कि 93 प्रतिशत अमेरिकी परिवारों के पास टीवी सेट थे, और जो फुटेज उन्होंने देखे वे पिछले संघर्षों की तुलना में कम सेंसर किये हुए थे और उन्हें तेज़ प्रसारित किया गया था। 1968 के बाद से, कवरेज काफी हद तक युद्ध के प्रतिकूल था। निर्दोष नागरिकों को मारे जाने, अपंग बनाने और प्रताड़ित करने की तस्वीरें टीवी और अख़बारों में दिखाई गईं, जिससे कई अमेरिकी भयभीत हो गए और युद्ध के ख़िलाफ़ हो गए।
पूरे देश में एक विशाल विरोध आंदोलन का जन्म हुआ। 4 मई, 1970 को ऐसे ही एक प्रदर्शन में, ओहियो में केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में नेशनल गार्ड्समैन द्वारा चार शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 'केंट स्टेट नरसंहार' ने अधिक लोगों को युद्ध के ख़िलाफ़ कर दिया। इन युवकों की मौत की छवियों और घर लौट रहे अमेरिकी सैनिकों के ताबूतों का जनता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध में लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए या लापता हो गए।
यह एक दुर्लभ संघर्ष था जिसमें अमेरिका ने कई भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया था। नेपलम (एक पेट्रोकेमिकल ज्वलनशील पदार्थ जो 2700C पर जलता है और जो कुछ भी छूता है उससे चिपक जाता है) और एजेंट ऑरेंज (जंगल में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य रसायन, लेकिन यह फ़सलों को भी नष्ट कर देता है और लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर करता है) के उपयोग ने ग्रामीण आबादी के बीच अमेरिका की छवि को बहुत नुक़सान पहुंचाया।
'खोजो और नष्ट करो' मिशन में अनगिनत निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया गया। वियतनाम युद्ध की सबसे कुख्यात घटना, 1968 के माई लाई नरसंहार में, अमेरिकी सैनिकों ने सैकड़ों वियतनामी नागरिकों को मार डाला।
केवल उत्तरी वियतनाम ही नहीं बल्कि दक्षिणी वियतनाम भी अमेरिका विरोधी था। दक्षिण में, अमेरिकी एजेंसियों, विशेषकर महिलाओं के साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। तथ्य यह है कि अमेरिकी वियतनाम में तैनात थे और दक्षिण वियतनामी सेना की कमान संभालते थे, लोगों के प्रति उनका रवैया इतना बुरा और अपमानजनक था कि सभी वियतनामी अमेरिका से नफ़रत करते थे।
जो हैं अपराधी उन्ही के हाथ में है फ़ैसला
आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध और अफ़ग़ानिस्तान पर हमला
11 सितंबर 2001 का दिन आधुनिक विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस दिन यह दुनिया एक बहुत बड़ी साज़िश का शिकार हुई थी। साम्यवाद के पतन के बाद यों तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया था और लगभग सभी देशों तथा विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रमुख विचारधाराओं ने उसकी महानता एवं श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था, परंतु इस्लाम एक ऐसी जीवन व्यवस्था है जो उसके रास्ते में एक स्थायी बाधा बनकर खड़ा था। अमेरिका का पूरा प्रयास इस जीवन व्यवस्था को अपने रास्ते से हटाकर बिना भागीदारी के विश्व पर शासन करना था। इस्लाम की जीवन प्रणाली इतनी मजबूत, व्यवस्थित, उदारवादी और मानव स्वभाव के अनुकूल थी कि तर्कों के आधार पर इसे त्रुटिपूर्ण बताना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने सभी पश्चिमी और ग़ैर-इस्लामी सरकारों की मदद से इस्लाम को बदनाम करने का वैश्विक अभियान शुरू किया। इस अभियान को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए अमेरिकी थिंक टैंक ने इस्लाम को किसी तरह से आतंकवाद से जोड़ने का फ़ैसला किया। इसके लिए हाई-प्रोफाइल साज़िशों का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया भर का मीडिया इस दिशा में काम करने लगा और इस्लाम विरोधी माहौल तैयार किया जाने लगा। फिर 11 सितंबर 2001 को चार हवाई जहाज़ों का बड़ी सफ़ाई से अपहरण कर लिया गया और उनमें से दो को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टकड़ा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेड सेंटर ध्वस्त हो गया। यह साज़िश इतनी कुशलता से रची गई थी कि इसकी ज़िम्मेदारी "इस्लामिक आतंकवादियों" के सर थोप दी गई। दुनिया भर के मीडिया ने बिना किसी सबूत के इस्लामी आतंकवाद के नाम पर अल-क़ायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना शुरू कर दिया। इस्लाम को आतंकवाद का धर्म साबित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया गया। इस हमले के लिए अल-क़ायदा नामक संगठन को ज़िम्मेदार ठहराया गया था और कहा गया था कि अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान ने अल-क़ायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पनाह दी रखी है।
इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू कर दिया, जिसे “वॉर ऑन टेरर” का नाम दिया गया। आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन लोगों से निपटने की योजना बनाई, जिनके बारे में उसकी थ्योरी थी कि वे अल-क़ायदा की तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों में सीधे तौर पर शामिल थे या अफ़ग़ान तालिबान के रूप में उस संगठन के सूत्रधार थे। आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध की शुरुआत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यह घोषणा करके "आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध में जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है।" पूरी दुनिया को सहयोग करने पर मजबूर कर लिया।
इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना और दुनिया भर में इस्लाम के ख़िलाफ़ माहौल और जनमत तैयार करना था। अमेरिका इस लक्ष्य में काफ़ी हद तक सफल रहा। दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा व्यक्त की जाने लगी। इस्लाम को रुढ़ीवादी, आउटडेटेड और अव्यावहारिक धर्म साबित करने आतंकवाद का स्रोत घोषित करने के लिए लेख लिखे जाने लगे, आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किए जाने लगे, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों, खासकर मुस्लिम युवाओं को परेशान किया जाने लगा। भारत जैसे देश में भी मीडिया ने इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलना शुरू कर दिया। मुस्लिम युवाओं को झूठे और निराधार आरोपों में गिरफ़्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेलों में डाला जाने लगा। हिंदूवादी नेता इस तरह के बयान देने लगे, "माना कि सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सभी आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं?" इन से भी आगे बढ़कर मुसलमानों की लिंचिंग का अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया।
यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध को लेकर बहुत गंभीर था। 9/11 हमले की जांच के नाम पर, अल-क़ायदा और (संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार) उस से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के लिए, उसने बगराम, अफ़ग़ानिस्तान और ग्वांतानामो बे, क्यूबा में यातनाशिविर बनवाए, जहां लोगों को अत्यधिक यातनाएं देकर उन अपराधों की ज़िम्मेदारी क़ुबूल कराने की कोशिश की जाती थी, जो उन्होंने किए ही नहीं थे। हालाँकि, हमले को एक निश्चित समय बीत जाने के बाद अमेरिकी ख़ुफ़या एजेंसी सीआईए के एक एजेंट ने अपनी मृत्यु शय्या पर खुलासा किया कि ट्रेड टावरों पर हमला संयुक्त राज्य अमेरिका की ही साज़िश थी।
उस साज़िश में शामिल 79 वर्षीय पूर्व सीआईए अधिकारी मैल्कम बोवार्ड ने अपने बयान में खुलासा किया कि 9/11 की घटना मुसलमानों को आतंकवादी करार देने की एक सोची-समझी योजना थी। उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ख़ाली करा लिया गया था। 13 जुलाई 2017 को योर न्यूज वायर (yournewswire.com) नाम की अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, मैल्कम ने स्वीकार किया है कि उसने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विस्फोटक रखे थे। जो विमान ट्रेड सेंटर की दो इमारतों से टकराए, वे रिमोट कंट्रोल का कमाल था और दोनों जहाज़ ख़ाली थे। उन विमानों के सिग्नल रिसीवर भी दोनों इमारतों में पांच अलग-अलग जगहों पर लगाए गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नष्ट करने के लिए पेंटागन में सीआईए मुख्यालय की इमारत में योजना बनाई गई थी। इस इमारत में एक विमान ट्रैक रिकॉर्डर स्थापित किया गया था, ताकि सुबूत लीक न हो सकें। मैल्कम स्वीकार करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के विनाश का दोष मुसलमानों पर लगाया गया था और इस अक्षम्य अपराध के लिए मुसलमानों का नरसंहार जारी है।
अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करके अमेरिका ने अपने कई शैतानी लक्ष्य पूरे किये। युद्ध के नाम पर न केवल अफ़गानों पर शांति हराम किए रखी, बल्कि पाकिस्तान (विशेषकर क़बायली इलाक़ों और ख़ैबर पख्तूनख्वा) के लोगों को भी इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका को यकीन था कि इस युद्ध की आड़ में वह इस क्षेत्र में रहकर अपने शिकार की बेहतर तरीक़े से निगरानी कर सकता है। भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह क्षेत्र अमेरिका के शैतानी लक्ष्यों के लिए अतीत की तुलना में अधिक उपयोगी साबित हुआ। 20 वर्षों तक वहां रह कर एक ओर उसका उद्देश्य भविष्य की आर्थिक महाशक्ति चीन पर नज़र रखना और उसे सबक सिखाना था। इसी तरह, वहां रहकर उसने आईएसआईएस के प्रभाव और पहुंच को भी बढ़ाया और मध्य एशियाई राज्यों के साथ पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर भी नज़र रखी। इन के अलावा अमेरीकियों ने उस पूरे क्षेत्र की सभी स्थानीय भाषाएं सीख लीं, जो सामरिक दृष्टि से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वह इस युद्ध में हर प्रकार की हानि उठाने से नहीं हिचकिचाता था।
यह युद्ध अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध है जिसमें 2,461 अमेरिकी सैनिक और 3,846 ठेकेदार मारे गये। अफ़ग़ानिस्तान की सेना और पुलिस के हताहतों की संख्या 66,000 बताई जाती है। इसी तरह नाटो गठबंधन देशों के 1144 सैन्यकर्मी मारे गये। आंकड़ों के मुताबिक, इस युद्ध में 47 हज़ार 245 अफ़ग़ानी नागरिक और तालिबान समेत अन्य प्रतिद्वंद्वी गुटों के 51,191 लोग मारे गए। बीस वर्षों तक चले इस युद्ध में 444 सहायता कर्मियों और 72 पत्रकारों की जान चली गयी। आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में कुल 1 लाख 72 हज़ार 403 लोग मारे गए। युद्ध पर 840 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुए। ऐसा कहा जाता है कि यह ख़र्चे न केवल युद्ध व्यय में सबसे अधिक है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खर्च की गई राशि से भी अधिक है।
9/11 की घटना को बाईस साल बीत चुके हैं। अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए हैं, लेकिन आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची है। दावा शांति और स्थिरता लाने का किया गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि 22 साल के इस लंबे युद्ध में अमेरिका 22 दिनों तक भी इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं कर सका। हामिद करज़ई दस साल से अधिक समय तक अफ़ग़ानिस्तान के कठपुतली राष्ट्रपति रहे। जाते-जाते करज़ई को भी यह विश्वास हो गया कि अमेरिका की महत्वाकांक्षाएँ वैसी नहीं हैं जैसी उसने यहाँ आते समय व्यक्त की थीं। हामिद करज़ई ने बार-बार यह सवाल उठाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अफ़ग़ान क्षेत्र में शांति लाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस हाथी के दांतों का प्रदर्शन कुछ और ही है। अफ़ग़ानिस्तान में इस्लामिक स्टेट (ISIS) की मौजूदगी के बारे में उन्होंने यहां तक कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में उक्त संगठन के लड़ाकों को अमेरिकी ठिकानों से हथियार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका के आगमन के बाद से देश में उग्रवाद और अस्थिरता बढ़ गई है। 2018 में अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार प्रांत में जब 9800 किलोग्राम का बम (सभी बमों की मां MOAB) गिराया गया तो करज़ई साहब इतने दुखी हुए कि उन्होंने औपचारिक रूप से अमेरिकी बलों की वापसी का आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी।
कब क्या हुआ
9/11 की घटनाएँ, फिर अफ़ग़ान धरती पर भीषण लड़ाई और अब अमेरिका के नेतृत्व में सभी विदेशी सैनिकों की वापसी और फिर तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा, पिछले 22 वर्षों में अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक झलक :
11 सितंबर, 2001: इस हमले में चार वाणिज्यिक विमानों का अपहरण कर लिया गया, जिनमें से दो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे दोनों इमारतें ढह गईं। तीसरा विमान पेंटागन की इमारत से टकराया, जबकि चौथा विमान अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इन घटनाओं में लगभग तीन हज़ार लोग मारे गये।
7 अक्टूबर: अमेरिका पर हमलों के बाद अमेरिकी सहयोगियों ने अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान और अल-क़ायदा के ठिकानों को निशाना बनाया। ये निशाने काबुल, कंधार और जलालाबाद जैसे बड़े शहरों पर हुए।
इससे पहले 1979 से 1989 तक सोवियत संघ ने अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़े की कोशिश की थी और दस साल तक चले उस युद्ध में अफ़ग़ान मुजाहिदीन सोवियत सेना को हराने में सफल रहे थे। हालांकि, इसके बाद सत्ता पर क़ब्ज़ा करने के लिए देश में गृहयुद्ध शुरू हो गया और 1994 में मुल्ला उमर के नेतृत्व में उभरे तालिबान ने 1996 में देश के बड़े हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया। ओसामा बिन लादेन ने तालिबान से शरण मांगी थी और तालिबान ने अमेरिकी मांग को खारिज करते हुए ओसामा बिन लादेन को उसे सौंपने से इनकार कर दिया था। परिणामस्वरूप, अमेरिका और सहयोगी सेनाओं ने हवाई हमले शुरू कर दिए जिसके कारण तालिबान की वायु सेना पूरी तरह नष्ट हो गई।
13 नवंबर 2001, काबुल गिर गया: उत्तरी गठबंधन, अफ़ग़ानिस्तान में एक तालिबान विरोधी समूह, गठबंधन बलों द्वारा समर्थित, काबुल में प्रवेश करने में कामयाब रहा, और 13 नवंबर 2001 तक, सभी तालिबान भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अन्य शहरों पर भी क़ब्ज़ा कर लिया गया।
26 जनवरी, 2004, नया संविधान: लोया जिरगा में लंबी बातचीत के बाद, नए अफ़ग़ान संविधान की पुष्टि की गई। इसी संविधान के आलोक में अक्टूबर 2004 में देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए।
7 दिसम्बर 2004 को हामिद करज़ई ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया
पोपलरज़ई दुर्रानी जनजाति के सदस्य हामिद करज़ई ने नए संविधान के तहत पहला चुनाव जीता और अगले पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने।
मई 2006, हेलमंद में ब्रिटिश सेना तैनात: अफ़ग़ानिस्तान के दक्षिण में तालिबान के गढ़ हेलमंद में ब्रिटिश सेना तैनात की गई थी। ब्रिटिश सैनिक क्षेत्र में चल रही निर्माण परियोजनाओं में मदद करने के लिए ज़िम्मेदार थे, लेकिन वहां की स्थिति के कारण, उन्हें सैन्य अभियानों में भाग लेना पड़ा, जिसके दौरान 450 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए।
17 फरवरी 2009, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई रणनीति: नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पदभार ग्रहण करने के बाद अफ़ग़ानिस्तान में और अधिक सैनिक भेजने की घोषणा की। अपने चरम पर, किसी भी समय अफ़ग़ानिस्तान में लगभग 140,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। अधिक सैनिक भेजने का अमेरिका का निर्णय इराक़ में इस्तेमाल की गई रणनीति पर आधारित था, जिसमें अमेरिकी सेना न केवल नागरिक आबादी की रक्षा करेगी बल्कि आतंकवादियों को भी नष्ट कर देगी।
2 मई, 2011, अल-क़ायदा नेता ओसामा बिन लादेन की मौत का नाटक: एक निराधार दावे के अनुसार, 9/11 के कथित मास्टरमाइंड और अल-क़ायदा नेता ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नौसेना सेल ने पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में उनके घर में मार डाला था। बाद में यह दावा किया गया कि उसका शव समुद्र में बहा दिया गया। (ताकि शव को दिखाना न पड़े, जो पहले से अस्तित्व में ही नहीं था।) इस दावे ने अल-क़ायदा नेता के लिए अमेरिका द्वारा एक दशक से चली आ रही खोज को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की उपस्थिति ने उन आरोपों को मज़बूत किया कि पाकिस्तान एक विश्वसनीय अमेरिकी सहयोगी नहीं था।
28 दिसंबर 2014, नाटो द्वारा युद्ध अभियान की समाप्ति: काबुल में एक समारोह के दौरान, नाटो ने आधिकारिक तौर पर अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध अभियान की समाप्ति की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने हज़ारों सैनिकों को वापस बुलाने का फ़ैसला किया, लेकिन जो सैनिक अफ़ग़ानिस्तान में तैनात रहे, वे अफ़ग़ान सेना को प्रशिक्षण देने के लिए ज़िम्मेदार थे।
2015, तालिबान की वापसी: तालिबान ने देश भर में आत्मघाती हमले फिर से शुरू कर दिए, साथ ही कार बम विस्फोट और अन्य हमले भी किए। काबुल में संसद भवन को भी निशाना बनाया गया, साथ ही कुंदुज़ पर भी हमले किए गए। दूसरी ओर, कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की आड़ में भी अफ़ग़ानिस्तान में विनाशकारी अभियान शुरू कर दिया गया।
25 जनवरी, 2019, मरने वालों की संख्या की घोषणा: अफ़ग़ान राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने घोषणा की कि 2014 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से पांच वर्षों में अफ़ग़ान सुरक्षा बलों के 45,000 से अधिक सदस्य मारे गए हैं। यह संख्या पहले के अनुमान से कहीं अधिक थी।
29 फरवरी, 2020, संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर: संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से क़तर की राजधानी दोहा में एक शांति बहाली समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार, अगर तालिबान समझौते का पालन करता है तो अमेरिकी और नाटो सेनाओं ने अगले 14 महीनों में अपने सभी सैनिकों को वापस लेने का फ़ैसला किया।
11 सितंबर, 2021, सेना वापसी की समय सीमा: संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह 9/11 की 20वीं बरसी पर अफ़ग़ानिस्तान से सभी सैनिकों को वापस ले लेगा। इस फ़ैसले के बाद नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसमें संशोधन किया और 31 अगस्त की तारीख़ तय की, जिसके मुताबिक़ सभी अमेरिकी कर्मी अफ़ग़ानिस्तान से वापस चले जाएंगे।
15 अगस्त, 2021, तालिबान का काबुल में प्रवेश: इस महीने, अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय बलों की वापसी के बाद, तालिबान तेज़ी से आगे बढ़े और अफ़ग़ानिस्तान को गृह युद्ध में झोंकने के अमेरिकी मंसूबे को नाकाम करते हुए अधिकांश हिस्से पर क़ब्ज़ा करना शुरू कर दिया। 14 अगस्त की शाम को कई प्रांतीय राजधानियों पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान काबुल के बाहरी इलाक़े तक पहुंच गए। अफ़ग़ान राजधानी पर तालिबान के तेज़ी से आगे बढ़ने की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी देश छोड़कर भाग गए और तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर क़ब्ज़ा कर लिया।
अब अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की इस्लामिक सरकार स्थापित हो गई है और इसका फल भी दिखाई देने लगा है। देश में हर स्तर पर अमन-चैन है, अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और देश समृद्धि की राह पर चल पड़ा है।
तालिबान का असली चरित्र: एक क़ैदी की आपबीती
अमेरिका तालिबान को आतंकवादी और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा घोषित करके उनका सफ़ाया कर देने पर उतारू था। पश्चिमी मीडिया का मिशन उनके ख़िलाफ़ नित-नया प्रोपेगैंडा करना और उन्हें मानवता के लिए ख़तरा साबित करना है, लेकिन वह मीडिया जो सच्चाई का झंडावाहक है वह भी तालिबान के पक्ष में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक तो इसलिए कि झूठ के इस हंगामे में सच की आवाज़ सुनेगा कौन और दूसरा इसलिए कि उसे इस अपराध के लिए कुचल कर न रख दिया जाए।
बहरहाल, तालिबान किस तरह के लोग हैं और उनके अस्तित्व से अमेरिका को असल ख़तरा क्या है, यह एक ब्रिटिश महिला पत्रकार के असाधारण अनुभव से पता चलता है। यवोन रेडली एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जो 28 सितंबर 2000 को गुप्त रूप से अफ़ग़ानिस्तान में दाखिल हुई और तालिबान ने उन्हें पकड़ लिया और 10 दिनों तक बंदी बनाकर रखा। इस कारावास ने उन्हें अविश्वास के जीवन से मुक्ति दिला दी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया और ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। आजकल वे इस्लाम की बहुत सक्रिय प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि मैं जहां भी जाऊं इस्लाम की रोशनी फैलाना चाहती हूं और लोगों में इस्लाम के लिए फैलाई गई पूर्वाग्रह की आग को बुझाना चाहती हूं।
इवोन रेडली लंदन के अखबार "संडे टाइम्स" में पत्रकार के रूप में काम करती थीं। जब अफ़ग़ानिस्तान पर अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं का हमला होने वाला था तो उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए अफ़ग़ानिस्तान जाने का फ़ैसला किया। इसी इरादे से वह पाकिस्तान पहुंची और वहां से उसने अफ़ग़ानिस्तान का वीजा लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रही, लेकिन वे आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध को लेकर इतनी उत्साहित थीं कि एक अफ़ग़ानी की मदद से फ़र्जी पहचान पत्र बनवाकर अफ़ग़ानिस्तान में घुस गईं। जब उनका गाइड उन्हें अपने गांव ले गया तो वहां के लोगों ने यवोन रेडली का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। जब ग्रामीणों को पता चला कि रेडली एक पश्चिमी महिला है तो वे डर गए, क्योंकि वहां बिना अनुमति के विदेशियों से संपर्क करना अपराध था, लेकिन अपने पारंपरिक आतिथ्य के प्रभाव में, उन्होंने रेडली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। फिर रेडली अपने गाइड के साथ निकल पड़ीं। वे दोनों कुछ दूर तक चले, फिर गाइड ने इवान रेडली को एक ख़च्चर पर बैठने के लिए कहा। रेडली ने सोचा कि पहाड़ी रास्ते पर चलने की अपेक्षा खच्चर पर बैठना बेहतर है। उनके बैठते ही खच्चर बिदक कर एक ओर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर, जब खच्चर रुका तो गाइड कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन सामने स्थानीय पोशाक में एक हथियारबंद आदमी खड़ा था। वह एक सुंदर युवक था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी।
इवान रेडली को बाद में पता चला कि वह एक तालिबान सैनिक था। उसने उनसे कैमरा ले लिया और उन्हें खच्चर से उतरने को कहा। इसी बीच और भी हथियारबंद तालिबानी वहां आ गये। यवोन रेडली का कहना है कि "उस समय मुझे लगा कि मैं दुनिया के सबसे क्रूर और दुष्ट आतंकवादियों की चपेट में हूं, अब मुझे नहीं पता कि वे मेरे साथ क्या करेंगे?"
उनके चारों ओर हथियारबंद लोग जमा हो गये, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ नहीं और किसी ने उनसे बात नहीं की। तभी तालिबान ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और आगे बढ़ गये। कुछ दूर चलने के बाद वे रुक गए। वहां बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। रेडली ने सोचा कि अब उनको संगसार किया जाएगा। इसी बीच कुछ बुदबुदाहट होने लगी, एक आदमी एक औरत के साथ इधर आ रहा था। महिला ने आते ही इवान रेडली के शरीर को टटोलना शुरू कर दिया। पता चला कि ये लोग इस महिला के आने का इंतिज़ार कर रहे थे ताकि वह आकर तलाशी ले सके।
रेडली कहती हैं कि उस समय मुझे लगता था कि मैं दुनिया के सबसे सभ्य देश की नागरिक हूं, लेकिन वहां महिलाओं के कपड़ों की तलाशी लेने में कोई कोताही नहीं बरती जाती, यानी आमतौर पर पुरुष सुरक्षाकर्मी ही महिलाओं के कपड़ों की तलाशी लेते हैं। दुनिया के ये सबसे अज्ञानी और क्रूर लड़ाके इस बात को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि एक महिला की तलाशी पुरुष को नहीं, बल्कि एक महिला को ही लेनी चाहिए। तलाशी के दौरान जब रेडली ने अपने कपड़े उठाए तो सभी लोग दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो गए।
गिरफ्तारी के बाद, यवोन रेडली ने समूह के एक सदस्य से सैटेलाइट फोन मांगा, ताकि वह अपने घर और कार्यालय को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सके। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो रेडली विरोध स्वरूप भूख हड़ताल पर बैठ गयीं। रेडली ने सोचा कि ये अत्याचारी और बर्बर लोग उनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह करेंगे। लेकिन रेडली को आश्चर्य तब हुआ जब लोगों को उनकी भूख हड़ताल की चिंता होने लगी और वे विभिन्न तरीकों से उनकी भूख हड़ताल खत्म करने की कोशिश करने लगे। तभी एक बुजुर्ग आए, उन्होंने काफी देर तक रेडली को अंग्रेजी में समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और लगातार खाने से इनकार करती रही। यह देखकर बुजुर्ग व्याकुल हो गए और जेल का माहौल बहुत भावुक हो गया। भूख हड़ताल के दौरान एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उनके लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। एक ऐसी सेना जिसके बारे में इवान रेडली ने केवल नकारात्मक बातें सुनी थीं और उसे पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना था, वह उनके सहानुभूतिपूर्ण रवैये से आश्चर्यचकित थी।
एक दिन उनका दुभाषिया, जो अंग्रेजी जानता था, उनके पास आया और बताया कि एक महान व्यक्ति उनसे मिलने आ रहे हैं। प्रवक्ता ने उनसे यह भी कहा कि वे उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। उसके जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यह भी अजीब था कि वह एक क़ैदी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने और बंद करने का अधिकार उसी के पास था और चाबी भी उसी के पास रहती थी। रेडली आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी हस्ती को देखकर वह थोड़ा डर गई, वह एक लंबा आदमी था, उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने एक लंबा गाउन पहना हुआ था, उसके चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा था। वह आदमी अनुमति लेकर कमरे में दाखिल हुआ और रेडली से उसका हालचाल पूछने के बाद उसने उससे इस्लाम के बारे में पूछा। रेडली ने सोचा कि अगर मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो रिहा होना मुश्किल होगा, इसलिए उसने बीच का बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है, इस्लाम शांति और सुरक्षा का धर्म है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, ''आप इस्लाम क़ुबूल क्यों नहीं कर लेतीं?'' इवान रेडली ने सोचा कि अगर वे अभी इस्लाम में आती हैं, तो यह समझ जाएगा कि दबाव में इस्लाम क़ुबूल किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जाने देंगे, तो मैं इस्लाम और क़ुरआन का अध्ययन करने का वादा करती हूं। जाते-जाते उस शख्स ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ही घर चली जाएंगी। अगली सुबह कुछ सैनिक आये और उसे ले गये। रेडली ने सोचा कि शायद उसे रिहा किया जा रहा है, लेकिन वे उसे महिला जेल में ले गए।
जब वह अंदर गयी तो उसने देखा कि कुछ यूरोपीय महिलाएँ एक घेरे में खड़ी होकर ज़ोर-ज़ोर से बाइबल का अध्ययन कर रही थीं। उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा था, क्योंकि इस्लामिक राज्य में ग़ैर-मुसलमानों को अपनी पूजा करने की पूरी आजादी होती है, केवल वे अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। जब रेडली धूम्रपान करना चाहती थी, तो महिलाओं ने उसे बताया कि यह धूम्रपान निषेध क्षेत्र है। एक दिन रेडली ने एक अधिकारी के सामने थूक दिया, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करना उसके लिए सामान्य बात थी। रेडली को लगा कि थूकने के लिए उसे फाँसी दे दी जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारे नेता के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि आज सभी क़ैदी अपने घर फोन करेंगे, लेकिन तुम्हें फोन करने की इजाज़त नहीं होगी। दुनिया की सबसे क्रूर सेना द्वारा दी गई इस सज़ा ने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया।
यवोन रेडली अपने कारावास के दौरान घटी एक दिलचस्प घटना का वर्णन इस प्रकार करती हैं: "हमारी जेल में बहुत कम पुरुष थे, केवल जेल के दरवाजे पर पहरा देने वाले ही पुरुष होते थे।" एक बार मैंने अपना अंडरवियर धोकर जेल के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक अधिकारी मेरे पास आया और मुझसे अंडरवियर वहां से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया।' इस पर उन्होंने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। लेकिन मुझे उन्हें परेशान करने में मजा आता था इसलिए मैंने ऊपर से कपड़ा हटा दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर इनके ऊपर कपड़ा डालोगे तो ये सूखेगा कैसे?
कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पास आया, उसने अपना परिचय अफ़ग़ानिस्तान के उप विदेश मंत्री के रूप में कराया। उन्होंने मुझसे वहां से अपना अंडरवियर हटाने का आग्रह किया और कहा कि यहां हमारे गार्ड हैं, अंडरवियर देखने से उनके मन में ग़लत विचार आ सकते हैं। उस समय मैं यही सोचती रह गई कि ये कैसे लोग हैं? कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और ब्रिटेन पूरी ताकत से उनके देश पर आक्रमण करने वाले हैं और वे मुझसे केवल इस डर से अंडरवियर हटाने के लिए बात करने आए हैं कि कहीं उनके रक्षकों के दिल में कोई ग़लत विचार न आ जाए। अमेरिकी हमले के दूसरे दिन तालिबान सैनिक रेडली के पास आये और कहा कि हम तुम्हें सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचा देंगे।
रेडली को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लोग हैं, इनके सिर पर मौत नाच रही है और इन्हें एक क़ैदी को यहां से सुरक्षित बाहर निकालने की चिंता हो रही है? फिर वे उसे सुरक्षित सीमा पर ले आए और पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया।
यवोन रेडली का कहना है कि अगर मैं किसी दूसरे देश की जेल में होती तो मैं ग्वांतानामो बे और अबू ग़रीब जेल के कैदियों की तरह होती। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत देखकर उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि वे अमेरिकी जेल में नहीं हैं। बाद में एवन रेडली ने डॉ. आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी के साथ उनकी रिहाई के लिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
रेडली ने कारावास के दौरान तालिबान से वादा किया था कि रिहा होने के बाद वे पवित्र क़ुरआन का अध्ययन करेंगी, इसलिए मुक्त होने के बाद, उन्होंने पवित्र क़ुरआन का अध्ययन करना शुरू कर दिया, साथ ही मानवाधिकारों और इस्लाम में महिलाओं के स्थान के बारे में भी पढ़ा।
इवोन रेडली का कहना है कि मुझे इस्लामोफोबिया के कारण अफ़ग़ानिस्तान भेजा गया था, मुझे क्या पता था कि इस्लाम मेरी आखिरी इच्छा बन जाएगा और मेरा जीवन इस्लाम को समर्पित हो जाएगा। अल्लाह मेरा समर्थक और मददगार हो और मुझे हमेशा सही रास्ते पर रखे।
कमज़ोरी के अपराध की सज़ा
इराक़ पर अमेरिकी हमले
20 मार्च 2003 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने इराक़ के ख़िलाफ़ एक अकारण और अवैध युद्ध शुरू करके 21वीं सदी के सबसे बड़े अपराधों में से एक की शुरुआत की। इस कमज़ोर देश के प्रतिरोध को तोड़ने और उसे हतोत्साहित करने के लिए उसके ख़िलाफ़ शुरू में ही भारी बल का उपयोग किया गया। हमारी भाषा में एक कहावत है, "जिसकी लाठी उसकी भैंस।" इराक़ पर अमेरिकी आक्रमण ऐसा ही एक हमला था। बुशवा गांव का दादा और चौधरी था। उसकी लाठी ने उसे सिद्दु की दूध देने वाली भैंस को हड़पने का अधिकार दे दिया था। एक दिन वह लाठी भांजता हुआ आया और रखवालों को मार-पीट कर सिद्दु की भैंस खोल ले गया। गांव वाले यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुशवा को रोके या टोके। सिद्दु बेचारा किससे शिकायत करता, शिकायत सुनने और निर्णय लेने का अधिकार भी तो चौधरी बुशवा को ही था।
ठीक उसी प्रकार अमेरिका की नज़र इराक़ के तेल भंडारों पर थी। दुनिया में अत्याचार और क्रूरता को प्रसारित करने के लिए उसे और संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए उसने उन पर क़ब्ज़ा करने की साज़िश रची। मीडिया प्रचार के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि इराक़ के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जिनका उपयोग वह दुनिया को नष्ट करने के लिए करना चाहता है, इसलिए इराक़ पर हमला करना और उन सभी हथियारों को निष्क्रिय करना आवश्यक है। फिर क्या था, इराक़ पर बम बरसने लगे।
अंग्रेजी में इस सैन्य रणनीति को (शॉक एंड ऑव) कहा जाता है। इस प्रकार, पीड़ित देश की सशस्त्र सेनाएँ पंगु हो जाती हैं, बिजली, पानी की आपूर्ति रोक दी जाती है, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति का उत्पादन बंद कर दिया जाता है और निरंतर बमबारी से उसका सामाजिक बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। इराक़ पर इस एकतरफ़ा बर्बर आक्रमण के परिणामस्वरूप दस लाख से अधिक लोग मारे गये।
उसके बाद तबाह हुए देश पर तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों से लैस 130,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों ने हमला कर दिया, जिसने संगठित इराकी प्रतिरोध के बचे-खुचे हिस्से को भी मिटा दिया और केवल दो सप्ताह के भीतर बगदाद पहुंच गए। फिर, एक और सप्ताह के नरसंहार के बाद, अमेरिकी सेना ने राजधानी पर क़ब्ज़ा कर लिया, आखिरी एकतरफा लड़ाई में सैकड़ों हज़ारों इराकियों के मुकाबले केवल 34 अमेरिकी हताहत हुए।
इराक़ में बुश प्रशासन द्वारा अपनाई गई युद्ध पद्धतियाँ पूरी तरह से आपराधिक थीं। युद्ध एक गुप्त हमले के साथ शुरू हुआ: क्रूज़ मिसाइलों से उन सरकारी इमारतों पर ताबरतोड़ हमले किए गए, जहां उनका मानना था कि इराकी शासक सद्दाम हुसैन मौजूद हैं, ताकि उन्हें मार डाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निषिद्ध हथियारों के उपयोग के साथ युद्ध जारी रहा। जैसे कि सफेद फास्फोरस बम जो शहरों में आग लगा देते थे और मानव मांस को बुरी तरह से जला देते थे। इसके अलावा, अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने घटिया यूरेनियम के अनुमानित 440,000 गोले गिराए, जो दीर्घकालिक कैंसर की दर को बढ़ाते हैं और भयानक जन्म दोषों का कारण बनते हैं।
युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यातना के सबसे भयानक रूप अबू ग़रीब जेल की चौंकाने वाली छवियों में सामने आए। इस भयावह यातना के लिए प्राधिकरण बुश प्रशासन के वकीलों द्वारा तैयार किया गया था जिन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति के पास कमांडर-इन-चीफ के रूप में लगभग असीमित शक्तियां हैं।
हमले और उसके आठ साल के क़ब्ज़े के बाद, डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस ने पूरे समुदाय के जानबूझकर विनाश को सामाजिक हत्या के रूप में परिभाषित किया। साम्राज्यवादी सनक ने मध्य पूर्व के सबसे विकसित देशों में से एक को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी विनाश की कगारपर पहुंचा दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने व्यवस्थित रूप से इराक़ में धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया और अमेरिकी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़ किसी भी एकजुट प्रतिरोध को रोकने के प्रयास में सुन्नी और शिया मुसलमानों और मुसलमानों और छोटे धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच सांप्रदायिक युद्ध को बढ़ावा दिया।
जानबूझकर आक्रामक युद्ध शुरू करके, अमेरिकी सरकार और उसके शीर्ष अधिकारी, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रिचर्ड चेनी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, कोंडोलीज़ा राइस और कॉलिन पॉवेल शामिल थे, युद्ध अपराधों के दोषी थे। ब्रिटिश प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर जैसे सहयोगियों के साथ, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित बुनियादी सिद्धांत का खुलेआम उल्लंघन किया।
हिंसा की इस कार्रवाई को लेकर दुनिया का एक तबका ऐसा था जो अमेरिका का विरोध कर रहा था और सवाल कर रहा था कि अमेरिका के पास इस हमले का क्या औचित्य है। इराक़ में किए गए भीषण विध्वंस के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसे सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसलिए मीडिया ने फिर से सफेद झूठ का सहारा लिया और इसे पूरी ढिठाई के साथ प्रचारित करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि वाशिंगटन ने इराक़ के विशाल तेल संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए इराक़ पर आक्रमण किया था। युद्ध के फ़ैसले लेने में उपराष्ट्रपति चेनी और बुश जैसे पूर्व तेल दिग्गजों के महत्व का उल्लेख किए बिना, न्यूयॉर्क टाइम्स लोगों को सद्दाम हुसैन के सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में व्यवस्थित झूठ पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी सावधानी से म लेते हुए सामूहिक विनाश के हथियारों के अभियान पर, जिसका उसने ख़ूब प्रचार किया था, किसी भी चर्चा से बचता रहा और पाठकों पर अपनी बनाई हुई स्टोरी थोपता रहा। अमेरिकी बुश प्रशासन के दावों की पुष्टि करती जूडिथ मिलर और माइकल गॉर्डन की रिपोर्ट जो सितंबर 2002 में टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई थी, को कॉर्पोरेट मीडिया द्वारा खूब प्रचारित और प्रसारित किया गया। अति तो यह है कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इन रिपोर्टों को इराक़ के ख़िलाफ़ सबूत के रूप में पेश किया था, जबकि वे खुद इराक़ पर हमलों के औचित्य के रूप में तैयार की गई थीं।
21 मार्च 2003 को, हमले शुरू होने के अगले दिन, वर्ल्ड सोशलिस्ट वेब साइट के अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष डेविड नॉर्थ ने युद्ध की प्रकृति का वर्णन करते हुए एक बयान प्रकाशित किया:
इराक़ पर अमेरिका का अकारण और अवैध आक्रमण एक ऐसी घटना है जो जीवन भर बदनामी में रहेगी। वाशिंगटन में राजनीतिक अपराधी जिन्होंने इस युद्ध को शुरू किया है और मीडिया के बदमाश जो नरसंहार का खेल रहे हैं, उन्होंने इस देश को शर्मसार कर दिया है। दुनिया के हर हिस्से में लाखों लोग एक क्रूर और बेलगाम सैन्य बल द्वारा एक छोटे और रक्षाहीन देश को घेरने के तमाशे से त्रस्त हैं। इराक़ पर आक्रमण शब्द के शास्त्रीय अर्थ में एक साम्राज्यवादी युद्ध है: संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय और कॉर्पोरेट कुलीनतंत्र के सबसे प्रतिक्रियावादी और रक्तपिपासु वर्गों के हितों में किया गया आक्रामकता का एक जघन्य कार्य। इसका स्पष्ट और तात्कालिक उद्देश्य इराक़ के विशाल तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना और उत्पीड़ित देश को अमेरिकी औपनिवेशिक शासन के अधीन लाना है।
यह युद्ध डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के तहत सोवियत संघ के विघटन के दौरान और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए आक्रमणों और कब्ज़ों की एक अंतहीन श्रृंखला का हिस्सा था। इस सीरीज की पहला खाड़ी युद्ध (1990-91) में हुआ था। फिर इनमें सर्बिया पर बमबारी (1999); अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण (2001); लीबिया पर बमबारी (2011) और सीरिया में अमेरिका समर्थित गृह युद्ध (2011) शामिल हैं। अमेरिकी पूंजीवाद की शक्ति को व्यक्त करने से दूर, अमेरिकी शासक वर्ग द्वारा दुनिया को जीतने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने का प्रयास उसके अपने गहन आंतरिक संकट से उपजा है।
मानवता का अपमान: ग्वांतानामो बे और अबू ग़रीब
मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून:
मानवता ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब दो विश्व युद्धों के रूप में मानवीय त्रासदियों का कटु अनुभव कर लिया, तो उसने यह निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकेने और मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेने के लिए एक संगठन बनाया जाए, जिसका नाम हो ‘संयुक्तराष्ट्र’। जब इस संयुक्तराष्ट्र के लिए चार्टर या दूसरे शब्दों में संविधान लिखा गया था तो उसमें कहा गया था कि वर्तमान विश्व में सभी लोगों को समान स्तर पर देखा जाएगा, सभी के मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी, मनुष्य की गरिमा और पवित्रता सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि सभी राष्ट्र, चाहे छोटे हों या बड़े, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किए गए समझौतों का पालन करेंगे।
1948 में संयुक्तराष्ट्र के इस चार्टर के अनुमोदन के बाद, पचास देशों की उपस्थिति में और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला ऐलेना रूजवेल्ट के नेतृत्व में मौलिक अधिकार निर्धारित किये गये जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए समान थे। ये मौलिक अधिकार संख्या में तीस हैं और जिस दस्तावेज़ में इन्हें सूचीबद्ध किया गया है उसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कहा जाता है। मानवाधिकारों की इस घोषणा में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और वे अपने पसंद की आस्था और विचारधारा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी आदमी दूसरे पर अत्याचार नहीं कर सकता। चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, सभी को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। कोई भी किसी को क़ैद, गिरफ़्तार या निर्वासित नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा करने का ठोस कारण न हो। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उस पर लगे आरोप साबित न हो जाएं।
संयुक्तराष्ट्र में इन मौलिक अधिकारों को मंजूरी मिलने के बाद युद्ध की स्थिति में युद्धबंदियों को मिलने वाले अधिकार भी निर्धारित किये गये। इन अधिकारों को परिभाषित करने के लिए 1949 में चार सम्मेलन आयोजित किए गए। उन्हें जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय कानून में एक दस्तावेज़ या समझौता है, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रत्येक देश समझौते का पालन करने के लिए बाध्य होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के लगभग सभी देशों ने युद्धबंदियों के लिए इन जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से तीसरे सम्मेलन में कहा गया है कि किसी भी युद्ध बंदी को यातना नहीं दी जा सकती या जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कन्वेंशन में आगे कहा गया है कि युद्धबंदियों को उचित भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उसके बाद संयुक्तराष्ट्र में अत्याचार के विरुद्ध कन्वेंशन भी प्रस्तुत किया गया, जो 1987 में लागू हुआ। यह कन्वेंशन कैदियों को प्रताड़ित करने पर रोक लगाता है। कुछ आपत्तियों के बाद अमेरिका ने अंततः उसे स्वीकार कर लिया है। इस सम्मेलन के अलावा, अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून भी हैं जो हिंसा को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं और मानव जीवन की गरिमा पर ज़ोर देते हैं।
विश्व कानून और विश्व शक्ति अमेरिका:
मानवाधिकारों और कैदियों के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय कानून आपको बताने का मकसद केवल यह बताना नहीं था कि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानूनों में क्या प्रगति हुई है, बल्कि हमारा मकसद ग्वांतानामो और अबू ग़रीब के यातनाशिविरों में होने वाले अमानवीय कृत्यों का जिक्र करने से पहले आपको एक छोटी सी तस्वीर देना था कि किन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत ये जेलें खोली गईं और फिर सालों तक चलती रहीं। ग्वांतानामो की जेल आज भी चालीस कैदियों को अपनी यातनाशिविर में क़ैद करके बैठी है। इसके अलावा, इन जेलों को इस विश्व शक्ति द्वारा नियमित रूप से खोला गया था, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का वाहक है और जिसकी प्रथम महिला की मौलिक मानवाधिकारों की घोषणा के निर्माण और अनुमोदन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
ग्वांतानामो एक अमानवीय यातनाशिविर ।
क्यूबा में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे ग्वांतानामो बे को जनवरी 2002 में 9/11 के बहाने शुरू हुए मुस्लिम-विरोधी युद्ध के कैदियों की यातना के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इस जेल में यातनाओं की ऐसी-ऐसी कहानियां बनीं कि जब वे कहानियां सामने आईं तो पूरी इंसानियत का सिर शर्म से झुक गया। अमेरिका की ख़ुफ़िया एजेंसी CIA ने इस जेल में यातना के नए तरीक़े ईजाद करने के लिए दो मनोवैज्ञानिकों, ब्रूस जेसन और जेम्स मिशेल को नियुक्त किया था। इन क्रूर मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हिंसा के ऐसे तरीक़े ईजाद किए कि उन्हें पढ़ने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इन तरीकों में शारीरिक यातना, अत्यधिक रोशनी और आवाज से यातना देना, कैदियों पर कुत्ते छोड़ना, उन्हें कई दिनों तक सोने न देना, यौन उत्पीड़न, पानी में गोता लगाना और हथकड़ी इतनी तेज बोंधना कि हाथ-पैर से खून निकल जाए। वहां रहने वाले कैदियों का कहना है कि उन्हें कई घंटों तक ऐसी स्थिति में रखा जाता था कि उन्हें बैठने, खड़े होने या लेटने की अनुमति नहीं होती थी। इन कैदियों के लिए सबसे दर्दनाक क्षण वह होता जब उन के सामने पवित्र क़ुरआन का अपमान किया जाता।
विडम्बना तो यह है कि उन यातनाओं से गुज़रने वाले ज़्यादातर क़ैदी ख़ुद अमेरिका के मुताबिक निर्दोष थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के मुताबिक, उस जेल में अब तक 780 कैदियों को रखा गया है, जिनमें से 730 को बिना किसी आरोप के रखा गया। उन पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया गया और उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस आरोप भी नहीं थे। ऐसे ही उस जेल ने उनकी ज़िन्दगी के कई साल निगल लिये। 780 कैदियों में से 40 अभी भी रिहाई का इंतिजार कर रहे हैं। यहां एकमात्र सवाल यह है कि उनके जीवन के उन अनमोल वर्षों को कौन वापस ला पाएगा जो ऐसे स्थान पर बर्बाद हो गए जहां जीवन ऐसा था कि जीवित लोग मृत्यु की प्रार्थना करते थे।
9/11 हमले के चार महीने बाद 1 जनवरी 2002 को, अफ़ग़ानिस्तान से कैदियों की पहली खेप ग्वांतानामो द्वीप पर अमेरिकी हिरासत केंद्र में लायी गई। दो दशक और युद्ध ख़त्म होने के बाद भी इस कैंप में कोई खास बदलाव नहीं आया है। मुहम्मद सालिही को अपने जीवन के 14 साल इसी जेल में गुज़ारने पड़े थे। उन्हें 70 दिनों तक यातना दी गई और लगातार तीन साल तक हर दिन 18 घंटे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी से पहले वे जर्मनी में रह रहे थे। जिन लोगों ने 9/11 के पूरे नाटक का मंचन किया, उन्हें ही सालिही पर अलक़ायदा के प्रमुख गुर्गों में से एक होने और 9/11 के हमलों में शामिल होने का संदेह था। लेकिन ये सभी आरोप अदालत में कभी साबित नहीं हो सके।
सालिही को 14 साल तक ग्वांतानामो बे यातनाशिविर में रखा गया था। इस दौरान, उन पर न तो आरोप लगाया गया और न ही दोषी ठहराया गया। मॉरिटानिया में जन्मे सालिही जब रिहा किया गया तो उनकी उम्र 50 साल थी, उनके जीवन के कीमती 14 साल जो उनसे छीन लिए गए, उसकी क़ीमत कोई नहीं चुका सकता।
सालिही का कुल अपराध यह था कि उसने अफ़ग़ानिस्तान में एक प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया और ओसामा बिन लादेन के सैटेलाइट फोन पर कॉल का जवाब दिया। न तो प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना कोई अपराध है, और न ही ओसामा बिन लादेन या किसी भी इंसान से बात करना अपराध है। हाँ, अमेरिकी दृष्टिकोण से, अगर वह एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर था, तो उस आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
सालिही की कहानी ग्वांतानामो बे हिरासत केंद्र में बंद ऐसे कई बंदियों और कथित संदिग्धों की कहानी है, जिनके लिए "सतत क़ैदी" शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जो 9/11 हमले के 20 साल बाद भी मुकदमे का इंतिजार कर रहे हैं। ग्वांतानामो के माध्यम से अमेरिका की जो छवि सामने आती है वह एक ऐसे देश की है जहां कानून के शासन की कोई अवधारणा नहीं है। बुश प्रशासन ने अमेरिकी कानून व्यवस्था से बचने के लिए ही विदेशों में जेलें बनवाईं और स्थानीय कानूनों के पालन का तो सवाल ही नहीं उठता।
अमेरिकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी द्वारा की गई जांच सहित अन्य जांचों से पता चला है कि ग्वांतानामो जेल में कैदियों को कितनी क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था। अल-क़ायदा के एक संदिग्ध अब्दुल रहीम अल-नाशिरी के वकील एंथनी नटले ने ग्वांतानामो हिरासत केंद्र की स्थिति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "हमें शर्म आती है कि वे सभी सिद्धांत नष्ट हो गए हैं जिनके आधार पर हमने एक स्वतंत्र देश बनाया था, जहां हर कोई समान रूप से न्याय का हकदार है। यह अत्यधिक खेद की बात है कि उसी देश ने उन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दीं और सब कुछ नष्ट कर दिया।”
ग्वांतानामो बे हिरासत केंद्र को देखना आसान नहीं है। जो पत्रकार इसे देखना चाहते हैं उन्हें इसके लिए नाकों चने चबाने पड़ते हैं। उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए, वाशिंगटन से साप्ताहिक चार्टर्ड उड़ानों को क्यूबा के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। विमानों को पहले क्यूबा के पूर्व में चक्कर लगाना पड़ता है। विमान को तब तक सैन्य अड्डे की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वह उतरने के लिए सही रनवे पर नहीं आ जाए। कई हफ्तों की सुरक्षा जांच के बाद डीडब्ल्यू को कुछ समय के लिए ग्वांतानामो जाने की अनुमति दी गई। प्रस्थान से पहले कई "नियमों" पर हस्ताक्षर कराए गए। इससे पत्रकारों को ग्वांतानामो की स्थिति का कुछ अंदाज़ा हो सकता है। वहां आंदोलन की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। जेल को बाहर से देखने की भी इजाजत नहीं है। डिटेंशन सेंटर के अंदर की सभी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। यह प्रक्रिया कैदियों के वकीलों के लिए बेहद परेशानी वाली है।
सवाल यह उठता है कि मानवाधिकारों और कानून के शासन के स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद यह जेल आज तक क्यों कायम है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद के ख़िलाफ़ चली लंबी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, अमेरिकी सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान से वापस लौट चुकी हैं। ऐसे में इस डिटेंशन सेंटर को बनाए रखने का क्या औचित्य है?
ग्वांतानामो बे हिरासत केंद्र को बंद करने की प्रारंभिक योजना जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के अंतिम दिनों में तैयार की गई थी। बराक ओबामा ने कई बार इसे बंद करने का वादा किया। लेकिन उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस में अपना बहुमत खो दिया था। रिपब्लिकन बहुमत ने एक कानून पारित किया,जिस कानून के अनुसार, ग्वांतानामो बे में रखा गया कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे किसी मुक़दमे के लिए हो या किसी चिकित्सीय आवश्यकता के तहत। इस कानून के द्वारा ग्वांतानामो बे के कैदियों को अमेरिका लाना असंभव बना दिया गया।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह घोषणा करके नीति को उलट दिया कि ग्वांतानामो हिरासत केंद्र खुला रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी के अनुसार, ग्वांतानामो संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवादी हमलों के ख़तरे से बचाता है। ग्वांतानामो बे को लेकर नया बदलाव मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में आया है। पदभार ग्रहण करने के बाद, बाइडेन ने अपने प्रवक्ता के माध्यम से घोषणा की कि वह कार्यालय में रहते हुए केंद्र को बंद करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब अमेरिकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें बाइडेन प्रशासन से कोई भी मौजूद नहीं था। सरकार अभी तक अपने वादे पर खरी उतरती नज़र नहीं आ रही है।
अबू ग़रीब, एक अमानवीय जेल:
2003 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक़ पर आक्रमण किया, तो उसने अपनी राजधानी में अबू ग़रीब नाम की एक जेल, (बल्कि यातनाशिविर) बनाई। इस जेल में सत्तर से अस्सी प्रतिशत क़ैदी भी निर्दोष थे। निर्दोष होने का मतलब यहां यह है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि पर अमेरिका के अवैध और अन्यायपूर्ण हमले के बाद भी अपनी मातृभूमि या स्वयं की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। यहां तक कि अमेरिकी बमों ने उन्हें और उनके परिवारों को उनकी आंखों के सामने नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सेना की ओर टेढ़ी नज़र से देखा तक नहीं। उन कैदियों को महज संदेह के आधार पर गिरफ़्तार किया गया था। इन कैदियों में कई महिलाएँ भी थीं जो क्रूर अमेरिकी सैनिकों की दरिन्दगी का शिकार हुई थीं। 2004 में जब उस जेल की तस्वीरें लीक हुईं तो मानवता कोप कर रह गई। एक तस्वीर में सिपाही एक क़ैदी के गले में रस्सी बांधकर उसे कुत्ते की तरह घसीट रहा था। इसी तरह एक अन्य तस्वीर में एक आदमी बिजली के नंगे तारों से क़ैदियों को झटका दे रहा था। अबू ग़रीब की उस जेल में क़ैदियों को नंगा करके एक-दूसरे के ऊपर इस तरह फेंक दिया जाता था, जैसे कबाड़ में पुराने टायरों को फेंक दिया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय विवाद और संयुक्तराष्ट्र की भूमिका
संयुक्तराष्ट्र की स्थापना 77 साल पहले 1945 में दुनिया के विभिन्न देशों के आपसी सहयोग स्थापित करने, दुनिया में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के साथ-साथ अन्य मानवीय मुद्दों जैसे मानवाधिकारों की सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास और पर्यावरण आदि पर सर्वसम्मति बनाने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में संयुक्तराष्ट्र की सफलता और विफलता की जाँच करने का एक तरीका यह है कि इस संगठन के कारणों और उद्देश्यों पर बारीकी से नज़र डाली जाए और फिर यह पता लगाया जाए कि ऐसे संगठन को विश्व शांति के लिए क्यों आवश्यक माना गया, जबकि ऐसा ही एक अन्य संगठन, राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स), बुरी तरह विफल हो चुका था। राष्ट्रसंघ की पूर्ण विफलता के बाद विश्व की शांति और सुरक्षा विनाश के कगार पर पहुँच गयी थी। इसलिए, प्रमुख शक्तियों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सख्त आवश्यकता महसूस हुई। 1943 की शुरुआत तक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन एक नए संगठन के पक्ष में थे। इसलिए, मॉस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद मूल रूप से एक विश्व संगठन की आवश्यकता पर सहमति हो गई। 1943 और 1944 के बीच, कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए, राहत और पुनर्वास, "खाद्य और कृषि", "इंटरनेशनल मानिट्री फंड" और "इंटरनेशनल एविएशन", ये गैर-विवादास्पद संगठन और सम्मेलन एक तरह की शुरुआत थे जिनके माध्यम से यह पता लगाया जा रहा था कि क्या विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के आयोजन की संभावना है या नहीं।
इसलिए, 1944 में, चार बड़ों के बीच बातचीत शुरू हुई। 1948 में लंबी चर्चा के बाद न्यायविदों की एक समिति ने एक मसौदा (Statute) तैयार किया। इस (Statute) को पचास देशों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाना था। दो महीने की कड़ी मेहनत और काफी चर्चा के बाद यह यूएन चार्टर अस्तित्व में आया। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क़ानून (Statute of international court) अस्तित्व में आया। विश्व की सर्वोच्च आशाओं पर आधारित यह संगठन 1945 में अस्तित्व में आया और संयुक्तराष्ट्र चार्टर पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किये गये। इस संस्था का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संगठन के निर्माण और योजना में अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व का बहुत बड़ा प्रभाव था और महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका के पास विशाल सैन्य और आर्थिक शक्ति है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का मानना था कि वैश्विक शांति अमेरिका के हित में है। यह भी माना जाता है कि इस संस्था की स्थापना में शक्तिशाली देशों में उच्च पदों पर बैठे लोगों का भी योगदान था।
द्वितीय विश्व युद्ध में तीन प्रमुख शक्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, यह आवश्यक समझा गया कि विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन महान शक्तियों को इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से भविष्य की सफलता के लिए एक-दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि युद्ध के दौरान सहयोग सफल रहा। इसलिए, इस अनुभव को उन्होंने संयुक्तराष्ट्र की सफलता के लिए एक आशा के रूप में देखा। "सैन फ्रांसिस्को" सम्मेलन में इन प्रमुख शक्तियों को अपने विभिन्न हितों और विचारों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला और उन प्रमुख शक्तियों ने एक-दूसरे को अपनी-अपनी स्थिति से अवगत कराया, कुछ समझौतों के बाद संयुक्तराष्ट्र चार्टर अस्तित्व में आया।
संयुक्तराष्ट्र चार्टर बनाने में महाशक्तियों का बहुत अधिक प्रभाव है। इसके अलावा इसमें महान युद्ध के बाद दुनिया की मनोवैज्ञानिक स्थिति और युद्ध के विनाश से बचाने के लिए एक ऐसे संगठन की ज़रूरत की इच्छा का भी योगदान है। संयुक्तराष्ट्र के इतिहास, संरचना, उसकी प्रकृति और उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि उस वार्ता में संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी और संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य पक्षों को प्रभावित करने के लिए अपना पूरा दबाव डाल रहा था। जाहिर तौर पर संयुक्तराष्ट्र को संपूर्ण वैश्विक समुदाय की एक एजेंसी के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय के साधन के रूप में बनाया गया था, ताकि संयुक्तराष्ट्र का दायरा और जवाबदेही विजयी राष्ट्रों के एक उप-संगठन होने तक सीमित न हो। संयुक्तराष्ट्र एक विशेष संगठन था जो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विवादों के अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया गया था। दुनिया के सभी लोगों और देशों के ऐसे झगड़े जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करते थे, इस संगठन के अधिकार क्षेत्र में आते थे। संयुक्तराष्ट्र का उद्देश्य न केवल विश्व की राजनीतिक समस्याओं से निपटना और शांति एवं व्यवस्था की समस्याओं पर नज़र रखना था, बल्कि इसके चार्टर के अनुच्छेद संख्या 1 में आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य मानवाधिकार के मुद्दे भी शामिल हैं। इस पहलू को "मेक्सिको" के प्रतिनिधि "स्क्विवेल पैडिलो" ने "सैन फ्रांसिस्को" सम्मेलन में इन शब्दों में व्यक्त किया:
“लोगो! यह चार्टर केवल युद्ध की भयावहता के ख़िलाफ़ सुरक्षा का एक उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो मानवीय गरिमा और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कल्याण और खुशी का चार्टर है। यह चार्टर ऐसी शांति का दावा करता है जो भय, निराशा, मानवीय अपमान और अन्याय और अभाव से मुक्त हो।''
संयुक्तराष्ट्र के इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब हम उन उद्देश्यों को देखते हैं जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। देखने वाली बात यह होगी कि उनमें वह कितना सफल रहा है। संयुक्तराष्ट्र के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बात यह जाती है कि इसकी स्थापना के इतने लंबे समय के बाद भी कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है, कारण चाहे जो भी हों, लेकिन दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है कि संयुक्तराष्ट्र की स्थापना के बाद से अब तक विभिन्न देशों के बीच 250 से अधिक युद्ध हो चुके हैं। संयुक्तराष्ट्र की उपलब्धियों में से एक यह है कि उसने वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने और विभिन्न देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास में अब तक 172 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्तराष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी सहायक संस्थाओं में से एक, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स ने 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों का आयोजन करके मानवाधिकारों और वैश्विक सुरक्षा के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई है। यह भी सच है कि संयुक्तराष्ट्र की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था WHO ने दुनिया में चेचक, पोलियो आदि जैसी कई बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने और महामारी को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाई है। संयुक्तराष्ट्र के बेहतर प्रदर्शन के पक्ष में एक बात यह भी जाती है कि इस विश्व स्तरीय संगठन की विभिन्न एजेंसियों और कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और सेवाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी सकारात्मक तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि संयुक्तराष्ट्र की ऐसी कई विफलताएँ हैं, जो इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की महत्ता और उपयोगिता पर सवाल उठाता है।
स्पष्ट है कि इस संगठन की सफलता पूरी तरह से हर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के सहयोग पर निर्भर है और आमतौर पर छोटे देशों को बड़ी शक्तियों द्वारा अपने हित में मिला लिया जाता है। संयुक्तराष्ट्र का निर्माण और पुनर्गठन वैश्विक शांति बनाए रखने का एक प्रयास था, लेकिन कमज़ोर देशों के सदस्यों को संयुक्तराष्ट्र के निर्णयों पर कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिया गया था। यही कारण है कि संयुक्तराष्ट्र का प्रदर्शन और रिकॉर्ड फ़िलिस्तीन, कश्मीर, साइप्रस, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के विवादों के मामले में विफलता की एक खुली किताब है। अगर आप आज विश्व में चल रहे विवादों को देखें तो यह अप्रभावी दिखाई देता है। रोहिंग्या मुसलमानों पर अमानवीय अत्याचार होता रहा, लेकिन संयुक्तराष्ट्र ने कोई कार्रवाई नहीं की।
संयुक्तराष्ट्र एक स्वायत्त संस्था नहीं है, न ही यह अपने सदस्य देशों की इच्छा के बिना कोई निर्णय ले सकता है। शायद इसका कारण यह है कि संयुक्तराष्ट्र में उन बुनियादी शक्तियों का अभाव है जो ऐसे निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। जब प्रस्तावों को लागू करने का समय आता है, तो संयुक्तराष्ट्र प्रमुख शक्तियों के "ब्लॉक" में विभाजित हो जाता है और संयुक्तराष्ट्र एक विभाजितराष्ट्र प्रतीत होता है। फिर लगभग सब कुछ विवाद में लिप्त राज्यों की इच्छा और तत्परता पर निर्भर करता है। संयुक्तराष्ट्र के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए भी विवाद में लिप्त दोनों राज्यों की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि कश्मीर के मामले में, जनमत संग्रह के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति आवश्यक है।
संयुक्तराष्ट्र का यह लक्ष्य कभी नहीं था कि इसे एक महान और सर्वोच्च राज्य बनाकर अन्य सदस्य देशों पर एक महाशक्ति के रूप में बैठा दिया जाए। ताकि वह अपनी नीति बल का उपयोग करके संकल्पों के रूप में युद्धरत सदस्य देशों पर थोप दे और इस प्रकार वैश्विक शांति और व्यवस्था स्थापित कर दे। जून 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति "रूजवेल्ट" ने कहा था, "हम एक सुपर-स्टेट बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसके पास कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना पुलिस बल हो और जिसके पास अन्य दमनकारी उपकरण और सहायक साधन हों, बल्कि हम एक प्रभावी समझौते और योजना की तलाश कर रहे हैं जिसे दुनिया भर के देश मिलकर कायम रखेंगे। वे अपनी स्थिति और शक्ति के अनुसार शांति और व्यवस्था बनाए रखने और युद्धों और संघर्षों को रोकने के लिए अपनी सेना तैयार रखेंगे और जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी वे मदद करेंगे।”
दूसरे शब्दों में, संयुक्तराष्ट्र उसी सीमा तक सफल होगा जिस सीमा तक शांतिप्रिय सदस्य देश अपनी इच्छा, योग्यता एवं क्षमता से सहायता कर सकेंगे। संयुक्तराष्ट्र दूसरे राज्यों के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संयुक्तराष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद क्रमांक 2 पैराग्राफ क्रमांक 2 के अनुसार यह संगठन सभी सदस्य देशों की संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित है। संयुक्तराष्ट्र स्वतंत्र राज्यों की एक सहकारी परियोजना है, यह राज्यों को पूर्ण 'सुपर स्टेट' के तहत ठोस आधारों पर बनाए रखने की एक अलग संरचना नहीं है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में संयुक्तराष्ट्र की सफलता और विफलता संगठन के सदस्य देशों की आंतरिक और बाहरी नीतियों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार वे वैश्विक स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।
संयुक्तराष्ट्र को महाशक्तियों के बीच गठबंधन की धारणा पर अस्तित्व में लाया गया था। यूएनओ चार्टर में प्रमुख शक्तियों को विशेषाधिकार और विशेष सम्मान दिए गए थे और उन्हें मानवीय जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं, लेकिन सबूत बताते हैं कि उन पाँच प्रमुख शक्तियों ने अपने "वीटो" का दुरुपयोग किया है और संयुक्तराष्ट्र के प्रस्तावों को अस्वीकार करके न्याय में बाधा डाली है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि महाशक्तियों ने कुछ वैश्विक मुद्दों में असहयोग की दरार को कम किया है। कुछ प्रमुख शक्तियों के बीच मज़बूत मतभेदों के कारण, अन्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान नहीं हो सका। पश्चिम और पूर्व के बीच विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच, "शीत युद्ध" इस लिए जारी रहा, क्योंकि उनकी अपनी-अपनी राजनीतिक और आर्थिक मौलिक अवधारणाएं अलग थीं और दृष्टिकोण भी अलग थे। ऐसे में दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। इस स्थिति को "द्विध्रुवी प्रणाली" कहा जाता है। यानी अमेरिका और उसके सहयोगी एक ओर और रूस और उसके सहयोगी दूसरी ओर। इस स्थिति ने संयुक्तराष्ट्र के लिए प्रस्ताव पारित करना कठिन बना दिया और उनके लिए वैश्विक विवादों का समाधान खोजना असंभव हो गया। इन दोनों खेमों के परस्पर विरोधी हित अंतर्राष्ट्रीय विवादों को प्रभावित करते हैं। वीटो का अधिकार एक और बड़ी बाधा रही है और छोटे राज्यों के लिए बहुत ही बेतुका है, जो संयुक्तराष्ट्र के समान सदस्य माने जाते हैं, लेकिन निर्णयों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।
बिग फाइव पॉवर्स की स्वीकृति की भी आलोचना की गई है और इसे संदेह की दृष्टि से देखा गया है कि संयुक्तराष्ट्र को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विशेष वर्ग द्वारा शासित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र द्वारा वैश्विक विवादों को हल करने के बजाय, पांच प्रमुख शक्तियों ने खुद को वैश्विक तानाशाह बनाने की साज़िश रची है। सम्मेलन के शुरुआती चरणों में पांच बड़े राज्यों की विशेष स्थिति के ख़िलाफ़ छोटे राज्यों की आवाज को दृढ़ता से खारिज कर दिया गया था।
संयुक्तराष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद विश्व में कई वैश्विक स्तर के राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए और सदस्य देशों में अनेक विवाद उत्पन्न हुए, लेकिन संयुक्तराष्ट्र ने एक भी विवाद सफलतापूर्वक हल नहीं किया है। संयुक्तराष्ट्र अकेले कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, न ही उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं। संयुक्तराष्ट्र आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं है। इस संस्था के वित्तीय संसाधन और पूंजी महाशक्तियों से आती है। महासचिव का पद भी स्वतंत्र नहीं है, उदाहरण के लिए सोवियत संघ के गंभीर अवरोध और हस्तक्षेप के कारण एक महासचिव को इस्तीफा देना पड़ा था। संयुक्तराष्ट्र के दूसरे महासचिव, "डॉग हम्मर्सचाइल्ड" (Dag Hammarskjöld) की रहस्यमय मौत भी संयुक्तराष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप के प्रति एक स्पष्ट प्रमाण है। संयुक्तराष्ट्र संघ के उद्भव के बाद से नई परिस्थितियों के कारण वैश्विक मामलों में उसकी भूमिका और प्रभाव बहुत सीमित हो गया है। "द्विध्रुवी" प्रतिस्पर्धा के कारण यूएनओ का प्रभाव लगातार कम होता गया है। एस हॉफमैन ने अपने एक लेख में इस स्थिति को इस प्रकार बताया है। जब भी दो बड़ी शक्तियों में से एक ने अकेले स्वतंत्र रूप से और बल या धमकी द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया तो यूएनओ अप्रभावी और सीमित रहा।
"हॉफमैन" की इस बात की पुष्टि हंगरी में सोवियत संघ की कार्रवाई से होती है। जहां यूएनयू ने हस्तक्षेप करने में पूरी कमज़ोरी दिखाई। संयुक्तराष्ट्र ने दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष के खतरों के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की सामूहिक सुरक्षा की तलाश नहीं की। अतीत में इन दोनों शक्तियों और उनके सहयोगियों के बीच कई खतरनाक संघर्ष हुए हैं, लेकिन उनमें संयुक्तराष्ट्र की भूमिका नाममात्र की रही है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रों ने "बर्लिन मालाकेड", लाओस युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध और कई अन्य खतरनाक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। भले ही ये दो महाशक्तियाँ सीधे तौर पर किसी संघर्ष में शामिल न हों, परोक्ष रूप से इन संघर्षों में उनके हित निहित होते हैं। फिर भी संयुक्तराष्ट्र कोई उपयोगी भूमिका निभाने में असफल रहा है। जैसा कि संयुक्तराष्ट्र 1960 में कांगो में और 1969 में मध्य पूर्व में अप्रभावी रहा। यूएनओ को दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध को समाप्त करने में विफलता के अलावा अन्य देशों के बीच विवादों को समाप्त करने में विफलता ही हाथ लगी। संयुक्तराष्ट्र की विफलता का कारण प्रमुख शक्तियों के बीच ठोस आधारों पर आम सहमति का अभाव और इच्छाशक्ति की अपरिपक्वता को माना जाता है। संयुक्तराष्ट्र की विफलता और निराशा का रिकॉर्ड बहुत लंबा और पुराना है। फ़िलिस्तीन, कश्मीर, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के मुद्दों पर संयुक्तराष्ट्र का प्रदर्शन और विफलता का रिकॉर्ड एक खुली किताब है। संयुक्तराष्ट्र के आर्थिक पक्ष पर गौर करें तो इस पक्ष में भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। बड़े और अमीर देशों के संसाधन और धन छोटे देशों को हस्तांतरित नहीं किए गए। UNCTAD का रिकॉर्ड भी बेहद दयनीय है।
संयुक्तराष्ट्र और मुस्लिम दुनिया
इस्लामी जगत के साथ संयुक्तराष्ट्र के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए हमें पिछली आधी सदी के दौरान इस्लामी जगत की आंतरिक स्थिति पर नज़र डालनी होगी और उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखना होगा जो मुस्लिम राष्ट्र को संयुक्तराष्ट्र से स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी। जिस समय संयुक्तराष्ट्र गठन और संगठन के चरण तय कर रहा था और वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के उत्थान और न्याय और सहिष्णुता को बढ़ावा देने को अपना लक्ष्य घोषित करके अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, उस समय मुस्लिम दुनिया के कई देश औपनिवेशिक शक्तियों की गुलामी से हाल ही में मुक्त हुए थे और कुछ मुस्लिम देश अभी भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के चरणों से गुजर रहे थे। जबकि मुस्लिम दुनिया के अधिकांश देश स्वतंत्र हो गए हैं और अपनी स्वतंत्र सरकारें स्थापित कर चुके थे, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां मुस्लिम राष्ट्र अभी भी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रों और देशों की सबसे बड़ी जरूरत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से स्थिरता हासिल करना, औपनिवेशिक युग की गुलामी के प्रभावों से छुटकारा पाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना था। जहां लंबे समय तक मुस्लिम देशों को गुलाम बनाए रखने वाले देश मुस्लिम दुनिया में अपना प्रभाव बनाए रखने और मुस्लिम देशों को राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, यहां तक कि विभिन्न मुस्लिम क्षेत्रों पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करने वाले औपनिवेशिक देशों, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल (और अब रूस) ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया है ताकि मुस्लिम दुनिया उनके प्रभाव से बच न सके और मुस्लिम देश उनके रिमोट कंट्रोल उपनिवेश बने रहें।
इस दृष्टिकोण से, मानवाधिकारों, न्याय और समानता के चैंपियन संयुक्तराष्ट्र से उचित तौर पर यह अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि वह बाहरी प्रभुत्व बनाए रखने और उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के इस संघर्ष में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे राष्ट्रों का समर्थन करेगा। लेकिन रिकॉर्ड गवाह है कि संयुक्तराष्ट्र न्याय और मानवाधिकार की इन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है, लेकिन वर्तमान वैश्विक संदर्भ यह है कि पश्चिमी देशों और मुस्लिम दुनिया के बीच प्रभुत्व बनाए रखने और उससे छुटकारा पाने के लिए यह संघर्ष एक स्पष्ट टकराव बन गया है जिसमें पश्चिमी देशों के लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित रूप से सामने हैं:
मुस्लिम देश वैचारिक एवं राजनीतिक एकता के लक्ष्य की ओर बढ़ने न पाएं।
परमाणु प्रौद्योगिकी और उन्नत सैन्य संसाधनों को मुस्लिम देशों की पहुंच से दूर रखा जाए।
सहायता और ऋण के नाम पर मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाए।
पश्चिमी हितों की रक्षा करने वाले मुस्लिम शासकों की हर क़ीमत पर रक्षा की जाए और मुस्लिम देशों की वैचारिक ताकतों को "कट्टरपंथी" घोषित करके सत्ता तक पहुँचने से रोका जाए।
मुस्लिम दुनिया की धार्मिक और सांस्कृतिक निरंतरता को कथित "मानवाधिकारों" के विपरीत घोषित किया जाए और इसके ख़िलाफ़ सामाजिक विद्रोह को प्रोत्साहित किया जाए।
यह सारा संघर्ष मुस्लिम दुनिया को पश्चिम की ग़ुलाम बनाए रखने और मुस्लिम देशों पर पश्चिम के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को जारी रखने के लिए है। और अगर इस संघर्ष के संदर्भ में संयुक्तराष्ट्र की भूमिका का यथार्थवादी विश्लेषण किया जाए तो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों, राष्ट्रों के बीच समानता, स्वतंत्रता और न्याय के तमाम दावों के बावजूद संयुक्तराष्ट्र इस संघर्ष में पूरी तरह से पश्चिमी उपनिवेशवाद का सहयोगी प्रतीत होता है। इसके अलावा, हमें संयुक्तराष्ट्र की स्थापना के बाद से मुस्लिम दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के संदर्भ में संयुक्तराष्ट्र के प्रदर्शन पर एक नज़र डालनी चाहिए।
फ़िलिस्तीनी जनता के मानवाधिकारों और इसराईल द्वारा बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करने के संबंध में संयुक्तराष्ट्र ने अपने स्पष्ट प्रस्तावों को नकारते हुए, वास्तव में इसराईल को सुरक्षा प्रदान की है, और संयुक्तराष्ट्र की संवेदनहीनता और आपराधिक लापरवाही के कारण, नस्लवादी इसराईल मनमानी कर रहा है।
कश्मीर में कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की स्पष्ट मान्यता के बावजूद, संयुक्तराष्ट्र कश्मीरियों के नरसंहार और उनके अधिकारों के उल्लंघन पर मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है और उन्हें आत्मनिर्णय का पूर्ण अधिकार देने में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहा है।
संयुक्तराष्ट्र ने हथियार प्रतिबंध के नाम पर बोस्निया की नवोदित सरकार को निहत्था करके बोस्निया में मुसलमानों के नरसंहार में भूमिका निभाई ताकि सर्ब सेना, जिसने पहले से ही पूर्व यूगोस्लाविया के सैन्य संसाधनों पर क़ब्ज़ा कर लिया था, बोस्नियाई मुसलमानों का स्वतंत्र रूप से नरसंहार कर सके।
संयुक्तराष्ट्र चेचन्या में मुसलमानों के नरसंहार के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सका है।
कजाकिस्तान में रूस के परमाणु परीक्षणों के दौरान कथित तौर पर 100,000 से अधिक मुसलमानों की दुखद मौत पर संयुक्तराष्ट्र पूरी तरह से चुप रहा।
खाड़ी युद्ध में इराक़ की सैन्य शक्ति को नष्ट करके, तेल संपदा को पश्चिमी देशों के खजाने में स्थानांतरित करके और खाड़ी में पश्चिमी देशों की सेनाओं को तैनात कर, संयुक्तराष्ट्र मुस्लिम दुनिया पर यह उल्टा एहसान जता रहा है कि उसने संकट आने पर मुस्लिम देश की जनता की मदद की ।
इनके अतिरिक्त सोमालिया और अजरबैजान सहित कई अन्य क्षेत्रों की समस्याओं का भी उल्लेख किया जा सकता है, जहां संयुक्तराष्ट्र ने मुस्लिम दुनिया के संबंध में अपना दोहरा मापदंड जारी रखा और औपनिवेशिक देशों ने संयुक्तराष्ट्र की छत्रछाया में मुस्लिम राष्ट्रों के ख़िलाफ़ अपने लक्ष्य हासिल किए।
और अंत में, संयुक्तराष्ट्र के नाम पर जो वैचारिक और बौद्धिक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका जिक्र करना अनुचित नहीं होगा। इसके माध्यम से इस्लामिक मान्यताओं और विचारधाराओं के ख़िलाफ़ और संयुक्तराष्ट्र चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को आधार बनाकर न केवल इस्लाम की मान्यताओं और नियमों की आलोचना की जा रही है, बल्कि मुसलमानों की सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को भी तहस-नहस करने की कोशिश की जा रही है। इस शीर्षक के तहत पश्चिमी लॉबी और वैश्विक मीडिया द्वारा इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ निरंतर अभियान का नक्शा इस प्रकार है:
सामाजिक अपराधों जैसे हाथ काटना, कोड़े मारना, क़सास (हत्या का बदला) और संगसार करने जैसी क़ुरआनी सजाओं को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है। जबकि बाइबल में इन अपराधों के लिए इन्ही सज़ाओं का वर्णन किया गया है।
विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर अल्लाह, रसूल और मज़हब की आलोचना के साथ-साथ अपमान की प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे इस्लामी जगत में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की निंदा करने वालों को पश्चिम में संरक्षण दिया जा रहा है। जिसका स्पष्ट उदाहरण सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और मिस्र के डॉ. अबू जैद के रूप में दुनिया के सामने है।
विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित मुसलमानों के पारिवारिक धार्मिक कानूनों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों और संयुक्तराष्ट्र चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं।
समलैंगिकता, विवाहेतर बच्चे पैदा करने और मुक्त यौन संबंध को वैध बनाने के लिए संयुक्तराष्ट्र के विश्व सम्मेलन मुस्लिम सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं।
इसी तरह, संयुक्तराष्ट्र मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ पश्चिमी उपनिवेशवाद के वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक युद्ध में पश्चिम के सहयोगी और साधन की भूमिका निभा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश मुस्लिम देशों की राजधानियों में जो लोग सत्ता में हैं, उनमें से अधिकांश पश्चिम के प्रतिनिधि और उसके हितों के रक्षक हैं। मुस्लिम दुनिया की दीनी तहरीकों और प्रबुद्ध वर्गों की ज़िम्मेदारी है कि वे इस स्थिति को समझें और मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ पश्चिमी उपनिवेशवाद के वैचारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आक्रमण की पृष्ठभूमि में संयुक्तराष्ट्र के व्यवहार का यथार्थवादी विश्लेषण करके दुनिया को इससे अवगत कराने की व्यवस्था करें।
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून:
युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून
युद्ध की परिभाषा
ओपेनहेम के शब्दों में, "युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अपने सशस्त्र बलों के माध्यम से एक-दूसरे पर हावी होने और विजेता की इच्छानुसार शांति की शर्तें लागू करने के उद्देश्य से किया जाने वाला विवाद है"।
स्टार्क का कहना है कि "अपने सबसे आम तौर पर समझे जाने वाले अर्थ में युद्ध मुख्य रूप से अपने सशस्त्र बलों के माध्यम से दो या दो से अधिक राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता है, जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी या प्रत्येक प्रतियोगी समूह का अंतिम उद्देश्य एक दूसरे को परास्त करना और शांति की अपनी शर्तों को लागू करना होता है"।
युद्ध के महत्वपूर्ण तत्व जो उपर्युक्त परिभाषाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं:
• युद्ध सशस्त्र बलों के बीच एक विवाद या हिंसा है।
• दो या दो से अधिक राज्य ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हों। जब एक ही राज्य के भीतर समूह एक-दूसरे का विरोध कर रहे हों तो इसे युद्ध नहीं कहा जा सकता।
• तीसरा, इसमें सशस्त्र बलों की भागीदारी होती है और युद्ध में ग़ैर-लड़ाकों को निशाना नहीं बनाया जाता है।
• युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य एक-दूसरे पर हावी होना होता है ताकि जीतने वाला राज्य दूसरे राज्य पर अपने नियम थोप सके।
संयुक्तराष्ट्र द्वारा वैध घोषित युद्ध का एकमात्र प्रकार आत्मरक्षा में लड़ा गया युद्ध है। हालाँकि, युद्ध के नियमों को केवल इसलिए निलंबित या अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी विशेष युद्ध को लड़ने का आधार ग़ैरक़ानूनी है। एक अवैध युद्ध में हमलावर और अन्य जुझारू दोनों को अपने व्यवहार को युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों, प्रथाओं और सम्मेलनों के अनुरूप बनाना होगा। साथ ही, कुछ अधिकारियों का सुझाव है कि एक जुझारू अपने दुश्मन द्वारा उन्हीं नियमों की अवहेलना के प्रतिशोध में युद्ध के कुछ नियमों की अवहेलना कर सकता है। यानी एक पक्ष अगर युद्ध के किसी नियम को तोड़ता है तो इससे दूसरे पक्ष को भी नियमों को तोड़ने का अधिकार मिल जाता है। यही वह बिन्दू है जिसके आधार पर व्यवहारिक रूप से युद्ध के सारे नियम व्यर्थ हो जाते हैं। यानी युद्ध के सारे नियम क़ानून की किताबों तक ही सीमित रह जाते हैं। मैदान पर युद्ध नियमों से नहीं, रणनिति से लड़ा जाता है और युद्ध की रणनीति किसी नियम और नैतिकता को नहीं मानती।
एनिमस बेलिगेरेन्डी
एनिमस बेलिगेरेन्डी का अर्थ है पार्टियों का इरादा। दो राज्यों के बीच युद्ध हो रहा है या नहीं, यह उन राज्यों की मंशा पर निर्भर करता है। जब राज्य एक-दूसरे से लड़ते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जब उनका ऐसा इरादा होता है तो वे युद्ध में होते हैं। तो, राज्यों की शत्रुता निम्नलिखित परिस्थितियों से प्राप्त की जा सकती है:
• सबसे पहले, जब राज्य स्वयं घोषित करते हैं कि वे युद्ध में हैं। यह एक उदाहरण है जो राज्यों की स्पष्ट मंशा को दर्शाता है।
• दूसरे, जब युद्ध की स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की जाती है, तो एक-दूसरे के साथ लड़ने वाले राज्य इसे युद्ध की तरह मानते हैं या राज्य बल के कुछ तरीक़े अपनाते हैं या युद्ध जैसी अन्य कार्रवाइयां अपनाते हैं या
• तीसरे राज्यों का मानना है कि दोनों राज्यों के बीच युद्ध चल रहा है, भले ही संबंधित राज्य इसे युद्ध मानें या नहीं।
युद्ध की घोषणा एक औपचारिक कार्य है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे के विरुद्ध मौजूदा या आसन्न युद्ध गतिविधि की घोषणा करता है। घोषणा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार की अधिकृत पार्टी द्वारा एक प्रदर्शनात्मक भाषण अधिनियम (या दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर) है।
युद्ध का नियम
कुछ उचित युद्ध सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के हिस्से के रूप में अपनाया गया है और युद्ध के कानून (यानी, अंतरराष्ट्रीय कानून) में शामिल किया गया है जो सशस्त्र बल का सहारा लेने, शत्रुता के संचालन और युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
उदाहरण के लिए, जिनेवा कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संधियों की एक श्रृंखला है जो ग़ैर-लड़ाकों, नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। संधियों पर 1864 और 1977 के बीच जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बातचीत की गई थी। पहला और दूसरा जिनेवा कन्वेंशन बीमार और घायल सैनिकों और नाविकों पर लागू होता है। इनमें घायलों और बीमारों के साथ-साथ चिकित्सा कर्मियों और परिवहन की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्धबंदियों पर लागू होता है, और चौथा जिनेवा कन्वेंशन क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों के लोगों पर लागू होता है। तीसरे कन्वेंशन में पर्याप्त भोजन और पानी सहित कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार की आवश्यकता है। चौथे कन्वेंशन में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो यातना और बंधकों को लेने से रोकते हैं, साथ ही चिकित्सा देखभाल और अस्पतालों से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
संयुक्तराष्ट्र और युद्ध
राष्ट्रों को युद्ध के बिना मुद्दों को हल करने के लिए मजबूर करने के प्रयास में, संयुक्तराष्ट्र चार्टर के निर्माताओं ने सदस्य देशों को केवल सीमित परिस्थितियों में, विशेष रूप से रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध करने का प्रयास किया।
25 जून 1950 को उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने के बाद संयुक्तराष्ट्र स्वयं एक युद्ध लड़ाका बन गया (कोरियाई युद्ध देखें)। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 9-0 के प्रस्ताव (सोवियत संघ की अनुपस्थिति में) द्वारा उत्तर कोरियाई कार्रवाई की निंदा की और अपने सदस्य देशों से दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए आने का आह्वान किया। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और 15 अन्य देशों ने एक "संयुक्तराष्ट्र बल" का गठन किया। 29 जून 1950 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस। ट्रूमैन ने इन शत्रुताओं को "युद्ध" नहीं बल्कि "पुलिस कार्रवाई" बताया।
संयुक्तराष्ट्र ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव जारी किए हैं, जिसमें कुछ युद्धों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी कार्रवाई घोषित किया गया है, विशेष रूप से संकल्प 678, 1991 के खाड़ी युद्ध को अधिकृत करता है जो कुवैत पर इराक़ के आक्रमण के कारण शुरू हुआ था। संयुक्तराष्ट्र के संकल्प "बल" या "सभी आवश्यक साधनों" के उपयोग को अधिकृत करते हैं।
युद्ध की घोषणा करने की योग्यता
युद्ध की घोषणा करने में कौन सक्षम है इसकी वैधता राष्ट्रों और सरकार के रूपों के बीच भिन्न होती है। कई देशों में, वह शक्ति राज्य के प्रमुख या संप्रभु को दी जाती है। अन्य मामलों में, युद्ध की पूर्ण घोषणा से कम कुछ, जैसे मार्के का पत्र या गुप्त ऑपरेशन, निजी लोगों या भाड़े के सैनिकों द्वारा युद्ध जैसे कृत्यों को अधिकृत कर सकता है। युद्ध की घोषणा के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को शत्रुता के उद्घाटन पर 1907 के हेग कन्वेंशन (III) में परिभाषित किया गया था।
1945 के बाद से, संयुक्तराष्ट्र चार्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून में विकास, जो अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में धमकी और बल के उपयोग दोनों को प्रतिबंधित करता है, ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध की घोषणाओं को काफी हद तक अप्रचलित बना दिया है, हालांकि ऐसी घोषणाओं की जुझारू या तटस्थ राष्ट्रों के घरेलू कानून के भीतर प्रासंगिकता हो सकती है।
संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद, अनुच्छेद 24 और 25 और चार्टर के अध्याय VII में दी गई शक्तियों के तहत, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या लागू करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को अधिकृत कर सकती है। संयुक्तराष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में यह भी कहा गया है कि: "अगर किसी राज्य के ख़िलाफ़ सशस्त्र हमला होता है तो वर्तमान चार्टर में कुछ भी व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को ख़राब नहीं करेगा।"
युद्ध उस स्थिति का नाम है जिसमें मानव निर्मित कानून अप्रभावी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि युद्ध, चाहे गृहयुद्ध के रूप में हो या किसी देश के भीतर विद्रोह के रूप में या देशों के बीच सैन्य हमले और प्रतिशोध के रूप में, तब होता है जब मामला कानूनों की सीमा से परे हो जाता है, या स्थिति कानून के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पहले अराजकता का माहौल होता है और फिर युद्ध होता है। युद्धरत ताकतें अपने हितों के लालच या दुश्मन के ख़िलाफ़ बदले की आग में इतनी अंधी हो जाती हैं कि उन्हें कानूनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। युद्ध में सभी प्रकार के असंयम की अनुमति है, इसलिए किसी राष्ट्र या सरकार से युद्ध के दौरान कानून का पालन करने की उम्मीद करना व्यर्थ है। पश्चिम के लोगों का दर्शन है कि "युद्ध और प्रेम में सब कुछ स्वीकार्य है।" उनके रचयिता और स्वामी ने उन्हें बनाया है। ये लोग युद्ध की स्थिति की तरह ही शांति की स्थिति में भी कानून के शासन का ध्यान रखते हैं। जाहिर है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हर पल अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ता है। जितना वे मैदान में दुश्मन से लड़ते हैं, उतना ही उन्हें अपने भीतर से भी लड़ना पड़ता है, जो उन्हें लगातार मौके का फायदा उठाने और दिल निकाल लेने के लिए प्रेरित करता है।
आख़िरत में विश्वास रखने वालों और न मानने वालों की लड़ाइयाँ अपने उद्देश्य, तरीक़े, नियमों और सीमाओं की दृष्टि से अलग-अलग होती हैं। जाहिर है, उनके परिणाम भी अलग-अलग होते हैं। ऐसी ही मानवीय कमज़ोरियों के तहत लड़े गए प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर पूरी दुनिया को गहरा अफ़सोस हुआ और अफ़सोस के दाग को मिटाने के लिए एक के बाद एक कई सम्मेलन आयोजित किए गए और भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए। लेकिन जब इन कानूनों को लागू करने का समय आया, तो सभी पीछे हट गए। एक का कानून तोड़ना दूसरे के लिए औचित्य बन गया। दो दशक भी नहीं बीते थे कि दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध का सामना करना पड़ा।
जब युद्ध समाप्त हुआ, तो लोगों को फिर से युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता के बारे में दृढ़ता से महसूस हुआ। उन्होंने पहले युद्ध के बाद किए गए प्रयासों को दोहराया। हालाँकि, जरूरत इस बात की थी कि लोगों में नैतिक भावना और ज़िम्मेदारी की भावना पैदा की जाए। ताकि वे बड़े पैमाने पर मानवता की भलाई के बारे में सोच सकें। लोग अपने सीमित स्वार्थ का त्याग कर सकें और दुनिया की व्यापक भलाई के लिए काम कर सकें। युद्ध के बारे में बड़े-बड़े आकर्षक और मनमोहक कानून हैं, लेकिन वे कानून की किताब तक ही सीमित हैं, वहां से कभी बाहर नहीं आते। युद्ध के मामले में दुनिया भर के देशों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ये हरकतें कानून की मौजूदगी का एहसास भी नहीं करातीं।
'युद्ध' कोई सीमाएँ और अधिकार क्षेत्र नहीं देखता। जब दो देशों के बीच या किसी देश के भीतर युद्ध या संघर्ष छिड़ जाता है तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि ऐसे समय में पहले से स्थापित कानून और नियमों का कड़ाई से अनुपालन नहीं होता है। ऐसे समय में ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनों का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि एक पश्चिमी विचारक मार्कस ट्यूलियस सिसरो ने भी कहा है, कि 'युद्ध के समय, कानून शांत हो जाते हैं।'
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) और इसके कन्वेंशन
जब हम आईएचएल के बारे में बात करते हैं, तो अधिकारों और नियमों के ये सेट विभिन्न सामाजिक तत्वों, उदाहरण के लिए, नागरिक व्यक्तियों, सामाजिक संरचनाओं और स्मारकों के ख़िलाफ़ जुझारू लोगों द्वारा देशों के बीच संघर्ष के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ताकतों के प्रभाव की दिशा और सीमा तय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि IHL राज्यों के बीच संघर्ष के समय में, ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में निहित अपने सभी आवश्यक प्रावधानों के साथ संचालन में आता है, जिन्हें अंततः युद्धरत राज्यों द्वारा एक-दूसरे के प्रति दिए गए शत्रुतापूर्ण व्यवहार को समाप्त करने और उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मूलभूत माना जाता है।
IHL के कार्यान्वयन से संबंधित नियम और कानून 1949 में चार जिनेवा सम्मेलनों में हस्ताक्षरित हुए। पहला जिनेवा कन्वेंशन क्षेत्र में घायलों और बीमारों की सुरक्षा से संबंधित है; दूसरा कन्वेंशन समुद्र में घायल, बीमार और जहाज़ के क्षतिग्रस्त सदस्यों की सुरक्षा से संबंधित है, तीसरा कन्वेंशन युद्ध के कैदियों की सुरक्षा से संबंधित है और चौथा कन्वेंशन युद्ध के समय में नागरिक आबादी की सुरक्षा से संबंधित है। ऐसा दावा किया जाता है कि आईएचएल उन राज्यों में शांति और मानवता का एक आवश्यक कानूनी उपकरण है जहां युद्ध के कारण विनाश की स्थिति पैदा हो जाती है।
196 देशों ने मान्यता दी
अपराधों को घरेलू संघर्ष या दो राज्यों के बीच युद्ध के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि नरसंहार और मानवता के ख़िलाफ़ अपराध शांतिकाल में या निहत्थे लोगों के समूह के प्रति सेना की एकतरफा आक्रामकता के दौरान हो सकते हैं। ऐसे कृत्यों की एक लंबी सूची है जिन्हें युद्ध अपराध माना जा सकता है। बंधकों को लेना, जान-बूझकर हत्या करना, युद्ध बंदियों के साथ अत्याचार या अमानवीय व्यवहार और बच्चों को लड़ने के लिए मजबूर करना कुछ उदाहरण हैं। जेनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर जो नियम बने, उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनेटिरियन लॉ कहा गया। इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। इसमें कुल 161 नियम हैं जिसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी है। युद्ध के दौरान इन नियमों का पालन करने के लिए सभी देश बाध्य हैं।
1949 में बनाए गए युद्ध के 161 नियम, अगर किसी जंग में तोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है युद्ध अपराध
युद्ध अपराधों के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। युद्ध के दौरान मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन को युद्ध अपराधों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के रोम संविधि द्वारा स्थापित परिभाषा 1949 के जिनेवा सम्मेलनों से ली गई है और इस विचार पर आधारित है कि व्यक्तियों को किसी राज्य या उसकी सेना के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
तीन सिद्धांतों पर आधारित
यह तय करने के लिए कि किसी व्यक्ति या सेना ने युद्ध अपराध किया है, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून तीन सिद्धांतों को निर्धारित करता है: भेद, आनुपातिकता और एहतियात। आनुपातिकता सेनाओं को अत्यधिक हिंसा वाले हमले का जवाब देने से रोकती है। "अगर एक सैनिक मारा जाता है, उदाहरण के लिए, आप जवाबी कार्रवाई में पूरे शहर पर बमबारी नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार ऐसे उद्देश्यों को लक्षित करना भी अवैध है जो "नागरिक जीवन के आकस्मिक नुक़सान, नागरिकों को चोट, नागरिक उद्देश्यों को नुक़सान पहुंचाते हैं। भेद का सिद्धांत कहता है कि आपको नागरिक और आबादी और वस्तुओं के बीच अंतर करना होगा। उदाहरण के लिए, एक बैरक पर हमला करना जहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वे अब संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं, एक युद्ध अपराध हो सकता है। अगर युद्ध बंदी बनाए भी जाते हैं तो उसके साथ मानवीय व्यवहार करना जरूरी है। अगर सड़क, ब्रिज, पावर स्टेशन और फैक्टि्रियों का इस्तेमाल सेना के द्वारा किया जा रहा है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है लेकिन अगर सेना नहीं है और शहर, इमारत को निशाना बनाया जाता है व बमबारी की जाती है तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा।
सबूतों को खोजने के लिए जांच
युद्ध के नियम के अनुसार अगर कोई देश युद्ध के दौरान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा। युद्ध के नियम के अध्याय 44 के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले देश के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। जब आईसीसी अभियोजकों के पास यह मानने का कारण होता है कि युद्ध अपराध किया गया है, तो वे उन सबूतों को खोजने के लिए एक जांच शुरू करते हैं जो उन अपराधों के लिए ज़िम्मेदार विशिष्ट व्यक्तियों को इंगित कर सकते हैं। हालांकि सबूत ख़राब हो सकते हैं या गायब हो सकते हैं। अभियोजकों के लिए इस तथ्य के बाद संदिग्ध युद्ध अपराधों की सफलतापूर्वक जांच करना बहुत मुश्किल है, जब संघर्ष के एक पक्ष ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की हो या गवाह आसपास नहीं हो।
युद्ध के तरीकों और साधनों की सीमाएँ
1907 के हेग कन्वेंशन से जुड़े विनियमों के अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि " शत्रु को घायल करने के साधन अपनाने का जुझारू लोगों का अधिकार असीमित नहीं है।" यह विशेष सिद्धांत इस क्षेत्र में अधिकांश कानून को रेखांकित करता है , और इसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, उसी संधि का अनुच्छेद 23 कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे ज़हर या जहरीले हथियारों का प्रयोग, दुश्मन लड़ाकों को विश्वासघात से मारना या घायल करना, आत्मसमर्पण करने वालों पर हमला करना, या यह घोषणा करना कि कोई क्वार्टर नहीं दिया जाएगा। यह अनावश्यक पीड़ा पैदा करने के लिए हथियारों, प्रोजेक्टाइल या सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस दृष्टिकोण का एक कारण, जैसा कि 1868 के सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा में कहा गया है , यह है कि "एकमात्र वैधयुद्ध के दौरान राज्यों को जिस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए वह दुश्मन की सैन्य ताकतों को कमज़ोर करना है ।
यह सिद्धांत, कुछ हद तक, कुछ हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध की व्याख्या करता है। इसलिए, का उपयोग1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल द्वारा रासायनिक और जीवाणुविज्ञानी हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । से1972 के बैक्टीरियोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में शामिल राज्यों ने किसी भी परिस्थिति में बैक्टीरियोलॉजिकल या जैविक हथियारों या विषाक्त पदार्थों को विकसित करने, उत्पादन करने, भंडारित करने, बनाए रखने या प्राप्त करने पर सहमति नहीं जताई। अगर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगा, तो संभवतः इसका स्वरूप भी वैसा ही होगा।
शत्रु लड़ाकों के विरुद्ध परमाणु हथियार का उपयोग किसी भी स्पष्ट निषेध के अधीन नहीं हैं। हालाँकि, कई अंतर्राष्ट्रीय वकील यह मानते हैं कि उनका उपयोग ऊपर बताए गए सिद्धांतों द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध है, क्योंकि विकिरण प्रभाव को न केवल ज़हर का एक रूप माना जा सकता है, बल्कि अनावश्यक पीड़ा पैदा करने के लिए तैयार किया गया एक हथियार भी माना जा सकता है । संयुक्तराष्ट्र की महासभा ने 1961 के संकल्प 1653 में उनके उपयोग की निंदा की , लेकिन इस प्रस्ताव का मूल्य इस तथ्य से काफी कमज़ोर हो गया है कि परमाणु हथियार संपन्न देशों में से केवल सोवियत संघ ने इसके लिए मतदान किया था। (1983), मेंशिमोडा बनाम जापान एक जापानी अदालत ने माना कि का उपयोगनागासाकी और हिरोशिमा के ख़िलाफ़ परमाणु हथियार अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत थे, न केवल इस्तेमाल किए गए हथियार के प्रकार के कारण बल्कि इसलिए कि उन दोनों शहरों की नागरिक आबादी पर किसी भी तरह से बमबारी 1907 के हेग कन्वेंशन के विपरीत थी ।
परमाणु हथियारों की तरह,आग लगानेवाला हथियारों पर तब तक विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता जब तक कि उनका उपयोग नागरिक आबादी के विरुद्ध न किया जाए। हालाँकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि दुश्मन लड़ाकों के ख़िलाफ़ उनका उपयोग (सैन्य उपकरणों के विपरीत) 1925 के जिनेवा गैस प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, क्योंकि वे "सभी समान तरल पदार्थ, सामग्री या उपकरणों" के नुस्खे के अंतर्गत आ सकते हैं ।
वियतनाम युद्ध ने उन खतरों को दर्शाया जो आधुनिक हथियार पर्यावरण के लिए पैदा कर सकते हैं । उस संघर्ष में रासायनिक जड़ी-बूटियों और वनों की कटाई के अन्य तरीकों के उपयोग के साथ-साथ मौसम के पैटर्न को बदलने के प्रयासों ने दुनिया का ध्यान ऐसी गतिविधियों की ओर आकर्षित किया। इसका परिणाम पर्यावरण संशोधन पर 1977 का संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन था, जिसके तहत राज्यों को व्यापक, लंबे समय तक चलने वाले या गंभीर प्रभाव वाले पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग में शामिल नहीं होने की आवश्यकता थी। पहला प्रोटोकॉल1977 का अधिनियम युद्ध के उन तरीकों या साधनों के प्रयोग पर भी रोक लगाता है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति पहुंचाना हो या होने की उम्मीद हो। इस प्रोटोकॉल द्वारा राज्यों को विशेष रूप से इस बात पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि क्या उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले कोई भी नए हथियार अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी भी नियम का उल्लंघन करेंगे।
समुद्र पर,नौसैनिक बल दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला कर सकते हैं। अर्जेंटीना के युद्धपोत का डूबनाइसलिए, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के आसपास ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कुल बहिष्करण क्षेत्र के बाहर हमला होने के बावजूद जनरल बेलग्रानो अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत नहीं था।
असैनिक
प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, केवल संघर्षरत पक्ष के सशस्त्र बलों के सदस्य ही शत्रुता में भाग ले सकते हैं, और कानून ने हमेशा वैध लड़ाके, जिस पर हमला किया जा सकता है, और नागरिक, जिसपर हमला नहीं हो सकता है, के बीच स्पष्ट अंतर निकालने का प्रयास किया है।
निम्न में से एक सशस्त्र संघर्षों में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के मौलिक नियम, जो 1978 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किए गए थे, नागरिक आबादी और संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष के पक्षों को हर समय नागरिक आबादी और लड़ाकों के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। हमले का निशाना न तो नागरिक आबादी होगी और न ही नागरिक व्यक्ति होंगे। हमले पूरी तरह से सैन्य उद्देश्यों के अनुरूप निर्देशित किये जायेंगे।” नागरिक आबादी के विरुद्ध रासायनिक या परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंधों पर ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा 1981पारंपरिक हथियार कन्वेंशन विशेष रूप से नागरिक आबादी के ख़िलाफ़ निर्देशित या अंधाधुंध उपयोग किए जाने वाले खानों, बूबी ट्रैप और अन्य समान उपकरणों और आग लगाने वाले हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, और 1977 का पहला प्रोटोकॉल नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत विस्तृत लक्ष्य प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, नागरिक आबादी को आतंकित करने के उद्देश्य के लिए की जाने वाली हवाई बमबारी निषिद्ध है, और इसलिए ऐसी भूमिका निभाने के लिए विमान का उपयोग अवैध होगा। सीमित परिस्थितियों में व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया जा सकता है, लेकिन यात्रियों, चालक दल और जहाज़ के कागजात को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद।
तटस्थ
1907 के पांचवें हेग कन्वेंशन में घोषणा की गई है कि तटस्थ शक्तियों का क्षेत्र अनुल्लंघनीय है और एक तटस्थ राज्य का कर्तव्य है कि वह एक युद्धरत राज्य को अपने क्षेत्र में संघर्ष करने से रोके। विशेष रूप से, एक जुझारू राज्य की सेना से संबंधित सैनिक जो तटस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उन्हें नज़रबंद किया जाना चाहिए। साथ ही, एक तटस्थ को सभी युद्धरत राज्यों के प्रति समान रूप से कार्य करना चाहिए; इस कारण से,यूनाइटेड किंगडम ने ईरान और इराक़ (1980-88) के बीच युद्ध में अपनी तटस्थता की घोषणा की, और दोनों पक्षों के सैन्य उपकरण बेचने से इनकार कर दिया, जिससे संघर्ष को लम्बा खींचने की उसकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी।
प्रतिबंधित वस्तुओं की ढुलाई की जांच के लिए ऊंचे समुद्रों पर तटस्थ शिपिंग को रोका जा सकता है (जैसा कि ईरान-इराक़ युद्ध में हुआ था जब एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज़ को ईरानी युद्धपोत द्वारा रोका गया था) । नौसैनिक युद्ध में, 1907 का 13वां हेग कन्वेंशन जुझारू लोगों को तटस्थ राज्य के क्षेत्रीय जल में सैन्य अभियान चलाने से प्रतिबंधित करता है , और तटस्थ लोगों पर स्वयं कर्तव्य लगाया जाता है कि वे युद्धरत राज्यों के युद्धपोतों की सहायता न करें।
युद्ध के निषिद्ध क्षेत्र
इस पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियां नहीं की जा सकतीं चंद्रमा (1979 की चंद्रमा संधि ),अंटार्कटिका (द1959 की अंटार्कटिक संधि ), या तटस्थ क्षेत्र (हवाई क्षेत्र सहित) या तटस्थ राज्यों के क्षेत्रीय जल पर। इसके अलावा, परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं कर सकते 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि ) या समुद्र तल पर रखा गया (द1971 की सीबेड संधि)।
युद्ध के क़ैदी
1949 का तीसरा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध बंदी को दी जाने वाली सुरक्षा की बुनियादी रूपरेखा प्रदान करता है । वह उस क्षण से सुरक्षित रहता है जब वह किसी दुश्मन के क़ब्ज़े में आ जाता है और अपनी अंतिम रिहाई और स्वदेश वापसी तक सुरक्षित रहता है। किसी भी प्रकार की जानकारी सुरक्षित करने के लिए उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता; उसे केवल अपना नाम, पद, जन्मतिथि और क्रम संख्या बतानी होगी। जब फ़ॉकलैंड्स संघर्ष के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा पकड़े गए एक अर्जेंटीना सेना अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि वह संघर्ष से पहले अर्जेंटीना में फ्रांसीसी और स्वीडिश नागरिकों के लापता होने के लिए ज़िम्मेदार था, तो उसे इस विषय पर जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका और उसे रिहा कर दिया गया।
युद्धबंदी सभ्य और मानवीय व्यवहार का हकदार है, उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, और हिरासत में लेने वाली शक्ति के सशस्त्र बलों के समान अधिकार और कर्तव्य दिए जाएं। युद्धबंदियों के विरुद्ध कोई प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता; उनके साथ कन्वेंशन के विपरीत व्यवहार नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई दुश्मन राज्य अपने युद्धबंदियों के साथ इस तरह का व्यवहार करता हो। अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और अन्य रैंकों को खतरनाक या अस्वास्थ्यकर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 1949 के तीसरे कन्वेंशन का अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि खदानों या इसी तरह के उपकरणों को हटाना खतरनाक श्रम माना जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि युद्धबंदियों को कन्वेंशन में निर्धारित उपचार दिया जाए, राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि:उनकी ओर से कार्य करने के लिए सुरक्षा शक्ति को नियुक्त किया जाता है। एक रक्षा शक्ति एक तटस्थ राज्य है जो युद्धबंदियों को रखने वाले राज्य को स्वीकार्य है। वियतनाम युद्ध या ईरान-इराक़ युद्ध के दौरान कोई सुरक्षा शक्तियां नियुक्त नहीं की गई थीं , लेकिन फ़ॉकलैंड संघर्ष में स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड किंगडम के लिए और ब्राजील ने अर्जेंटीना के लिए काम किया। कोई राज्य इसकी अनुमति दे सकता है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (ICRC) एक वैकल्पिक सुरक्षा शक्ति के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा, आईसीआरसी को युद्धबंदी शिविरों का दौरा करने का भी अधिकार है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध बंदी पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना है (अनुशासनात्मक दंड दिए जाने के बजाय) तो सुरक्षा शक्तियों (या आईसीआरसी) को सूचित रखा जाना चाहिए, ताकि रक्षा करने वाली शक्ति को आरोपी के लिए एक वकील मिल सके। अगर मौत की सज़ा दी जाती है, तो फ़ैसले के बाद और सुरक्षा शक्ति को सज़ा की सूचना दिए जाने के बाद कम से कम छह महीने तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है। युद्ध बंदी पर पकड़ने से पहले किए गए किसी अपराध (जैसे युद्ध अपराध) के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन दोषी पाए जाने पर भी वह युद्ध बंदी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का हकदार है।
भागने की कोशिश कर रहे युद्धबंदियों के ख़िलाफ़ हथियारों का इस्तेमाल एक चरम उपाय है और इससे पहले चेतावनी दी जानी चाहिए। हिरासत में लेने वाली शक्ति को युद्धबंदी की मौत की जांच करनी चाहिए और सुरक्षा शक्ति को सूचित करना चाहिए। फ़ॉकलैंड्स संघर्ष में ऐसी घटना घटी, जब एक ब्रिटिश सैनिक ने अर्जेंटीना के एक युद्ध बंदी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। परिणामी जांच में सैनिक को बरी कर दिया गया और आईसीआरसी को एक रिपोर्ट भेज दी गई।
शत्रुता के समापन पर युद्धबंदियों को स्वदेश भेजना होता है । कोरियाई युद्ध के समापन पर समस्याएँ उत्पन्न हुईं जब कई उत्तर कोरियाई लोग वापस लौटना नहीं चाहते थे। 1953 में एक प्रत्यावर्तन आयोग की स्थापना की गई और युद्ध के शेष कैदियों को इसमें स्थानांतरित कर दिया गया। शत्रुता समाप्त होने से पहले युद्ध के सक्षम कैदियों को वापस भेजना आम बात हो गई है। एक सीमित सीमा तक यह ईरान-इराक़ युद्ध में हुआ, लेकिन यह फ़ॉकलैंड संघर्ष की एक प्रमुख विशेषता थी।
पेशा
द्वितीय विश्व युद्ध यह दर्शाता है कि क़ब्ज़े वाले क्षेत्र में नागरिक युद्ध के कानूनों से काफी हद तक असुरक्षित थे। परिणामस्वरूप, 1949 के चौथे जिनेवा कन्वेंशन ने उनकी सुरक्षा के लिए विस्तृत नियम प्रदान किए। एक संरक्षित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, जो किसी भी समय और किसी भी तरीक़े से, किसी संघर्ष या क़ब्ज़े की स्थिति में, खुद को संघर्ष के किसी पक्ष या सत्ता पर काबिज होने वाले व्यक्ति के हाथों में पाता है, जिसका वह नागरिक नहीं है। इसलिए, क़ब्ज़े वाले क्षेत्र के निवासी कन्वेंशन के तहत संरक्षित व्यक्ति हैं; वे मानवीय व्यवहार और अपने व्यक्ति, सम्मान, पारिवारिक अधिकारों, धर्म, शिष्टाचार और रीति-रिवाजों के प्रति सम्मान के हकदार हैं। चौथे कन्वेंशन का अनुच्छेद 34 विशेष रूप से बंधकों को लेने और उनके या उनकी संपत्ति के ख़िलाफ़ प्रतिशोध पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 49 संरक्षित व्यक्तियों के क़ब्ज़े वाले क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण पर रोक लगाता है जब तक कि, अनिवार्य सैन्य कारणों की इतनी मांग है। जून 1967 के युद्ध के बाद, इसराईल ने वेस्ट बैंक , ग़ज़्ज़ा पट्टी और गोलान हाइट्स में क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया , लेकिन उसने दावा किया कि चौथा कन्वेंशन उन पर लागू नहीं होता है। संयुक्तराष्ट्र ने 1988 में प्रस्तावों में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जब उसने विशेष रूप से घोषणा की कि यह कन्वेंशन 1967 से इसराईल द्वारा क़ब्ज़ा किए गए सभी फ़िलिस्तीनी और अन्य अरब क्षेत्रों पर लागू है। इन प्रस्तावों में इन क्षेत्रों में कई इसराईली प्रथाओं की निंदा की गई, जैसे इसराईली शासन के ख़िलाफ़ विद्रोह के दौरान फ़िलिस्तीनी नागरिकों (जो चौथे कन्वेंशन के तहत संरक्षित व्यक्ति हैं) की हत्या, घायल और निर्वासन के रूप में ।
संरक्षित व्यक्ति जो सशस्त्र बलों के सदस्य नहीं हैं और जो क़ब्ज़ा करने वाली सेना के ख़िलाफ़ बल का उपयोग करते हैं, वे विशेष उपचार के हकदार नहीं हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर वे युद्धबंदी की स्थिति के हकदार नहीं हैं। कब्ज़ा करने वाला राज्य उन पर क्षेत्र के सामान्य कानूनों या उसके द्वारा लगाए गए कानूनों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चला सकता है। हालाँकि, अगर ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा देनी है, तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि संरक्षित व्यक्ति पर क़ब्ज़े वाले के प्रति निष्ठा का कोई कर्तव्य नहीं है। साथ ही, जो राज्य किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लेता है, उसे उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संयुक्तराष्ट्र के विभिन्न प्रस्ताव इसकी पुष्टि करते हैं; नवंबर 1988 में महासभा के एक प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई कि "1967 से यरुशलम सहित फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसराईल का कब्ज़ा, किसी भी तरह से उन क्षेत्रों की कानूनी स्थिति में बदलाव नहीं करता है।"
नरसंहार
नरसंहार , जातीयता , राष्ट्रीयता , धर्म या नस्ल के कारण लोगों के एक समूह का जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश । समकालीन अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार का अपराध "मानवता के विरुद्ध अपराध" की व्यापक श्रेणी का हिस्सा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण (नूर्नबर्ग चार्टर) के चार्टर द्वारा परिभाषित किया गया था। चार्टर ने न्यायाधिकरण को नेताओं पर अभियोग लगाने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। नागरिकों के ख़िलाफ़ अमानवीय कृत्यों के साथ-साथ राजनीतिक, नस्लीय या धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के कृत्यों और अन्य प्रकार के अपमानजनक आचरण के अंतर्राष्ट्रीय अपराधीकरण में भी योगदान दिया। नाज़ी शासन द्वारा बनाई गई गतिनूर्नबर्ग परीक्षणों और नाजी अत्याचारों के आगामी खुलासों के कारण संयुक्तराष्ट्र (यूएन) महासभा द्वारा संकल्प 96-I (दिसंबर 1946) पारित किया गया , जिसने नरसंहार के अपराध को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय बना दिया, और संकल्प 260-III ( दिसंबर 1948), जिसने के पाठ को मंजूरी दी।
सम्मेलन का अनुच्छेद 2 नरसंहार को इस प्रकार परिभाषित करता है
किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कार्य, जैसे: (ए) समूह के सदस्यों की हत्या; (बी) समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुक़सान पहुंचाना; (सी) जानबूझकर समूह पर जीवन की ऐसी स्थितियाँ थोपना जिससे उसका संपूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश हो सके; (डी) समूह के भीतर जन्मों को रोकने के इरादे से उपाय लागू करना ; (ई) समूह के बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
नरसंहार के कमीशन के अलावा, सम्मेलन ने नरसंहार में साज़िश, उकसावे, प्रयास और सहभागिता को भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय बना दिया।
नरसंहार सम्मलेन की आलोचना
हालाँकि इस सम्मेलन को लगभग सर्वसम्मत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है और हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार, नरसंहार का निषेध अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य मानदंड ( जस कॉजेंस [लैटिन: "सम्मोहक कानून"]) बन गया है, फिर भी यह सम्मेलन अक्सर आलोचना का शिकार होता रहा है। नरसंहार के संभावित पीड़ितों की सूची से राजनीतिक और सामाजिक समूहों को बाहर करने की आलोचना की गई। कहा गया "सम्मेलन की नरसंहार की परिभाषा का जानबूझकर खंड" - वह भाग जिसमें "एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे" का उल्लेख है - भी समस्याग्रस्त है । सबसे आम आपत्तियों में से दो यह हैं कि इस तरह के इरादे को स्थापित करना मुश्किल हो सकता है और व्यक्तियों को ऐसे इरादे सौंपने का प्रयास आधुनिक समाजों में बहुत कम समझ में आता है, जहां हिंसा गुमनाम सामाजिक और आर्थिक ताकतों के साथ-साथ व्यक्तिगत विकल्पों के कारण भी हो सकती है।
नव गतिविधि
इसके अनुसमर्थन के बाद पहले 50 वर्षों के दौरान, नरसंहार सम्मेलन में प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव था, इस तथ्य के बावजूद कि इसमें संयुक्तराष्ट्र को इसे लागू करने में सक्षम बनाने के प्रावधान शामिल थे। हालाँकि सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया था कि नरसंहार के आरोप वाले व्यक्तियों पर अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायाधिकरण या उस राज्य के न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिसमें अपराध किया गया था, 21 वीं सदी की शुरुआत तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई स्थायी दंड न्यायाधिकरण मौजूद नहीं था, और घरेलू स्तर पर मुकदमा चलाया गया था।
नरसंहार सम्मेलन पहली बार 1993 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष लागू किया गया था, जब बोस्निया और हर्जेगोविना की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि यूगोस्लाविया का संघीय गणराज्य सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा था। 1990 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नरसंहार के कथित अपराधों पर मुकदमा चलाने में और अधिक सशक्त हो गया । संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलग-अलग न्यायाधिकरणों की स्थापना की पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटीवाई) और रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटीआर), दोनों ने नरसंहार के अपराध के भौतिक तत्वों के साथ-साथ इसके कमीशन के लिए व्यक्तिगत आपराधिक ज़िम्मेदारी स्थापित करने वाले मानदंडों को स्पष्ट करने में योगदान दिया।
उदाहरण के लिए, रवांडा ट्रिब्यूनल ने कहा कि नरसंहार में "लोगों के एक समूह को निर्वाह आहार देना, घरों से व्यवस्थित निष्कासन और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को न्यूनतम आवश्यकता से कम करना शामिल है। " इसने यह भी फ़ैसला सुनाया कि "बलात्कार और यौन हिंसा नरसंहार है ।।। जब तक वे एक विशेष समूह को, पूर्ण या आंशिक रूप से, नष्ट करने के विशिष्ट इरादे से प्रतिबद्ध हो, इस तरह लक्षित" - जैसा कि रवांडा संघर्ष में हुआ था, जहां हुतु जातीय समूह के प्रभुत्व वाली सरकार ने एचआईवी संक्रमित पुरुषों द्वारा जातीय तुत्सी महिलाओं के सामूहिक बलात्कार का आयोजन किया। इरादे के महत्वपूर्ण मुद्दे पर,यूगोस्लाव ट्रिब्यूनल ने यह भी फ़ैसला सुनाया कि नरसंहार का इरादा लोगों के छोटे समूहों के साथ-साथ बड़े समूहों के उत्पीड़न में भी प्रकट हो सकता है।
1 जुलाई 2002 को रोम संविधि लागू हुई1998 में लगभग 120 देशों द्वारा रोम में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) लागू हुआ। आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नरसंहार का अपराध शामिल है, और क़ानून अपराध की वही परिभाषा अपनाता है जो नरसंहार सम्मेलन में पाई गई है। आईसीसी की स्थापना - हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका , चीन और रूस की भागीदारी के बिना - नरसंहार के अपराध को दबाने और दंडित करने के लिए ज़ोरदार और ठोस प्रयासों के पक्ष में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सहमति का एक और संकेत था।
2009 में ICC ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर पर पश्चिमी सूडान के दारफुर क्षेत्र में युद्ध अपराध और मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के आरोप लगाए गए हैं। बशीर पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए दूसरा गिरफ्तारी वारंट 2010 में जारी किया गया था। 2019 में गाम्बिया ने म्यांमार के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें उस देश पर रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक के व्यवस्थित उत्पीड़न के लिए नरसंहार का आरोप लगाया गया ।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है क्या?
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि (The Rome Statute) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। दरअसल 17 जुलाई, 1998 को 120 देशों ने मिलकर एक क़ानून तैयार किया जिसको नाम दिया गया - The Rome Statute। इसी कानून के तहत एक संस्था बनाने की बात कही गई - जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1 जुलाई, 2002 को आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना की गई। इसका उद्द्येश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिये ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करना साथ ही, इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है।
ICC से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
आमतौर पर ICC चार प्रकार के अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करता है - नर-संहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामक अपराध। अंग्रेज़ी में कहें तो - genocide, war crimes, crimes against humanity and the crime of aggression। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और अभी मौजूदा वक़्त में इसके 123 सदस्य देश हैं। दुनिया भर में 123 देश इस ICC के सदस्य हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे देश इसके सदस्य नहीं है। इन सभी देशों की अपनी अपनी कुछ शर्ते हैं। बात भारत की करें तो भारत ऐसा मानता है कि ICC का सदस्य बनने से उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकता है। साथ ही भारत आईसीसी से कुछ अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण भी चाहता है जैसे कि इसके साक्ष्य संग्रह में कठिनाई है; यहां पर निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव है और अपराध की परिभाषा में इसकी अस्पष्टता है। इन्हीं सब मुद्दों के चलते भारत ने ICC की सदस्यता अभी स्वीकार नहीं की है।
ICC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
ICC संयुक्तराष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन यह संयुक्तराष्ट्र के साथ सहयोग करता है। संयुक्तराष्ट्र संघ से संबंधित सिविल मामलों का एक कोर्ट अलग से है जिसका नाम है - अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ)। ये देशों के बीच के आपसी विवादों पर सुनवाई करता है। आईसीजे को किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या उसे गिरफ़्तार करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। शायद इसीलिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) की स्थापना की गई। ये व्यक्तियों से सम्बंधित मामलों की सुनवाई करता है।
अपने फ़ैसले को लागू करवाने के लिए ICC के पास खुद का कोई पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। यानी एक कोर्ट के रूप में अपने आपको फंक्शन कराने के लिए यह अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर रहता है।
ICC केवल सदस्य देशों के मुकदमों या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है तथा इसमें मामले की सुनवाई की कुछ शर्ते भी निर्धारित की गईं हैं जैसे कि
• जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उस मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जाँच करने से इनकार कर दिया गया हो।
• जब सयुंक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा किसी मुद्दे को आई।सी।सी। के पास भेजा गया हो।
निष्कर्ष
ICC की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्याय सामाजिक संघर्षों के केंद्र में है और यह दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और न्यायसंगत विकास में योगदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ICC आरोपों से परे है। ऐसे में जरूरत है कि अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये ICC संयुक्तराष्ट्र के स्थायी सदस्यों को शामिल करके और जांच एवं अभियोजन को और सशक्त बनाकर अपनी स्थिति मज़बूत करे।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की दादागीरी
जब हम दुनिया में होने वाले युद्धों के इतिहास पर नज़र डालते हैं,विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद के ज़माने पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आता है, जो दुनिया में होने वाले लगभग सभी युद्धों में किसी न किसी रूप में लिप्त है। यों तो अमेरिका का पूरा इतिहास रक्तरंजित है और 245 वर्ष के उसके इतिहास में शांति के केवस 17 वर्ष हैं, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हंसते-खेलते दो नगरों पर एटम बम गिराकर उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर दिया तो दुनिया उससे नफ़रत करने और उसको प्रतिबंधित करने के बजाय उससे डरने और उसकी चापलूसी करने लगी। फिर क्या था अमेरिका दुनिया का दादा बन बैठा और अपना हित साधने के लिए हरेक के मामले में टांग अड़ाने लगा। 1945 से 2001 तक, दुनिया के 153 क्षेत्रों में हुए 248 सशस्त्र संघर्षों में से 201 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किए गए थे, जो कुल संख्या का 81 प्रतिशत है। युद्धों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने छद्म युद्धों का समर्थन करके, सरकार विरोधी विद्रोहों को भड़काकर, हत्याएं करके, हथियार और गोला-बारूद प्रदान करके और सरकार विरोधी सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देकर अन्य देशों के मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया है, जिससे इसमें शामिल देशों की सामाजिक स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुक़सान हुआ है। चूँकि ऐसी गतिविधियाँ संख्या में बड़ी हैं और पूरी सीमा सार्वजनिक नहीं की गई है, उन सभी के संबंध में विशिष्ट डेटा एकत्र करना कठिन है।
दो दशक पहले, 7 अक्टूबर 2001 को, तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिकी बमबारी अभियान की शुरुआत ने अफ़ग़ान लोगों के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न पैदा कर दिया था। अल-क़ायदा और तालिबान से मुकाबला करते समय, अमेरिका ने बड़ी संख्या में अनावश्यक नागरिक हताहत भी किये। अप्रैल 2021 में द चाइना सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज द्वारा प्रकाशित दूसरे देशों के ख़िलाफ़ अमेरिकी आक्रामक युद्धों के कारण हुई गंभीर मानवीय आपदाओं के अनुसार, अमेरिकी सैनिक 30,000 से अधिक नागरिकों की मौत का कारण बने, 60,000 से अधिक को घायल किया और लगभग 110 लाख लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर किया। काबुल विश्वविद्यालय के विद्वानों का अनुमान है कि अफ़ग़ानिस्तान युद्ध में प्रति दिन लगभग 250 लोग हताहत हुए और देश को प्रति दिन 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुक़सान हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा छेड़े गए आक्रामक युद्धों में से केवल एक है।
अमेरिका की दादागीरी का कच्चा चिट्ठा यहां प्रस्तुत करने का इरादा है। देखना यह है कि पन्ने कहां तक अनुमति देते हैं :
1945-1947: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी सेना को हटाने की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिकों ने मुख्य भूमि चीन में मोर्चाबंदी की।
1946: ट्राइस्टे, (इटली): यूगोस्लाव पीपुल्स आर्मी द्वारा वेनेज़िया गिउलिया के ऊपर उड़ान भर रहे एक अमेरिकी सेना परिवहन विमान को मार गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जोनल क़ब्ज़े वाली रेखा पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाने और उत्तरी इटली में वायु सेना को मज़बूत करने का आदेश दिया। इससे पहले अमेरिकी नौसैनिक इकाइयों को घटनास्थल पर भेजा जा चुका था।
1948: बर्लिन: बर्लिन एयरलिफ्ट 24 जून, 1948 को सोवियत संघ द्वारा बर्लिन के अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों की लैंड नाकाबंदी के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मई 1949 में नाकाबंदी हटाए जाने तक बर्लिन में हवाई आपूर्ति की।
1948-1949: चीन: जब शहर कम्युनिस्ट सैनिकों के क़ब्ज़े में आ गया तो अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा के लिए नौसैनिकों को नानकिंग भेजा गया, और अमेरिकियों की सुरक्षा और निकासी में सहायता के लिए शंघाई भेजा गया।
1950-1953: कोरियाई युद्ध: संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरियाई आक्रमण का जवाब उसकी सहायता से दिया। सक्रिय संघर्ष के अंतिम वर्ष (1953) के दौरान कोरिया में तैनात अमेरिकी सेना की संख्या 300,000 से अधिक हो गई। कार्रवाई में 36,600 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए।
1950-1955: फॉर्मोसा (ताइवान): जून 1950 में, कोरियाई युद्ध की शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी सातवें बेड़े को फॉर्मोसा पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हमलों और मुख्य भूमि चीन के ख़िलाफ़ चीन गणराज्य के सशस्त्र बलों के संचालन को रोकने का आदेश दिया।
1950: प्यूर्टो रिको (संयुक्त राज्य अमेरिका का औपनिवेशिक क्षेत्र): यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल गार्ड ने प्यूर्टो रिको के स्वतंत्रता सेनानियों, जो अमेरिकी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना चाहते थे के ख़िलाफ पी-47 थंडरबोल्ट हमले वाले विमान, भूमि-आधारित तोपखाने, मोर्टार फायर और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।
1954-1955: चीन: पहला ताइवान जलडमरूमध्य संकट, नौसेना इकाइयों ने टैचेन द्वीप समूह से अमेरिकी नागरिकों और सैन्य कर्मियों को निकाला।
1955-1964: वियतनाम: पहला सैन्य सलाहकार 12 फरवरी 1955 को वियतनाम भेजा गया। 1964 तक, अमेरिकी सेना का स्तर 21,000 तक बढ़ गया था।
1956: मिस्र: स्वेज संकट के दौरान एक समुद्री बटालियन ने अलेक्जेंड्रिया से अमेरिकी नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को निकाला।
1958: लेबनान: 1958 लेबनान संकट, बाहर से समर्थित विद्रोह के ख़तरे से बचाने में मदद के लिए राष्ट्रपति केमिली चामौन के निमंत्रण पर नौसैनिकों को लेबनान में उतारा गया। राष्ट्रपति की कार्रवाई को 1957 में पारित कांग्रेस के एक प्रस्ताव द्वारा समर्थन दिया गया था जिसने दुनिया के उस क्षेत्र में ऐसी कार्रवाइयों को अधिकृत किया था।
1959-1960: क्यूबा क्रांति के बाद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कैरेबियन (दूसरा समुद्री ग्राउंड टास्क फोर्स) तैनात किया गया था।
1955-1975: वियतनाम युद्ध: अमेरिकी सैन्य सलाहकार एक दशक तक दक्षिण वियतनाम में थे, और साइगॉन सरकार की सैन्य स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी संख्या बढ़ती चली गई। राष्ट्रपति लिंडन बी। जॉनसन ने अगस्त 1964 में "दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्रता और शांति की रक्षा" का समर्थन करने के लिए अमेरिकी दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव मांगा। जिसमें कांग्रेस द्वारा युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना, राष्ट्रपति जॉनसन को दक्षिण पूर्व एशिया में पारंपरिक सैन्य बल के उपयोग की अनुमति दी गई। इस प्रस्ताव के बाद, और मध्य वियतनाम में एक अमेरिकी प्रतिष्ठान पर कम्युनिस्ट हमले के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल 1969 तक युद्ध में अपनी भागीदारी को 543,000 सैन्य कर्मियों के शिखर तक बढ़ा दिया।
1962: क्यूबा: क्यूबा मिसाइल संकट, 22 अक्टूबर को, राष्ट्रपति कैनेडी ने सोवियत संघ से क्यूबा के लिए आक्रामक मिसाइलों की खेप पर "संगरोध" की स्थापना की। उन्होंने सोवियत संघ को यह भी चेतावनी दी कि पश्चिमी गोलार्ध में देशों के ख़िलाफ़ क्यूबा से किसी भी मिसाइल का प्रक्षेपण सोवियत संघ पर अमेरिकी परमाणु प्रतिशोध का कारण बनेगा।
1962-1975: लाओस: अक्टूबर 1962 से 1975 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाओस में कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों के सैन्य समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका सीआईए अर्धसैनिक बलों का उपयोग करके एक गुप्त सैन्य अभियान लड़ रहा था, जिसे गुप्त युद्ध के रूप में जाना जाता था।
1964: कांगो (ज़ैरे): संयुक्त राज्य अमेरिका ने विद्रोह के दौरान कांगो के सैनिकों को एयरलिफ्ट करने और विदेशियों को बचाने के लिए बेल्जियम के पैराट्रूपर्स को ले जाने के लिए चार परिवहन विमान भेजे।
1965: डोमिनिकन गणराज्य पर आक्रमण: ऑपरेशन पावर पैक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डोमिनिकन विद्रोह के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और 20,000 अमेरिकी सैनिकों को भेजा क्योंकि यह डर बढ़ गया था कि क्रांतिकारी ताकतें तेज़ी से कम्युनिस्ट नियंत्रण में आ रही थीं। जब अमेरिकी नौसैनिक बलपूर्वक सैन्य शासन को कायम रखने के लिए उतरे तो क्रांति कुचल दी गई।
1967: इसराईल: यूएसएस लिबर्टी घटना, जिसके बाद 8 जून, 1967 को इसराईल रक्षा बलों द्वारा संयुक्त राज्य नौसेना के तकनीकी अनुसंधान जहाज़ पर हमला किया गया, जिसमें 34 लोग मारे गए और 170 से अधिक अमेरिकी चालक दल के सदस्य घायल हो गए।
1967: कांगो (ज़ैरे): संयुक्त राज्य अमेरिका ने विद्रोह के दौरान कांगो केंद्र सरकार को साजोसामान सहायता प्रदान करने के लिए चालक दल के साथ तीन सैन्य परिवहन विमान भेजे।
1968: लाओस और कंबोडिया: अमेरिका ने कंबोडिया और लाओस के संप्रभु राष्ट्रों में हुची मिन्ह मार्ग के लक्ष्यों के ख़िलाफ़ गुप्त बमबारी अभियान शुरू किया। बमबारी कम से कम दो साल तक चलती रही।
1970: कंबोडियन अभियान: अमेरिकी सैनिकों को कंबोडिया में कम्युनिस्ट अभयारण्यों को साफ करने का आदेश दिया गया था, जहां से वियत कांग और उत्तरी वियतनाम ने वियतनाम में अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेना पर हमला किया था। 30 अप्रैल से 30 जून तक चले इस हमले का उद्देश्य दक्षिण वियतनाम से अमेरिकी सेना की लगातार सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना और वियतनामीकरण के कार्यक्रम में सहायता करना था।
1972: उत्तरी वियतनाम: क्रिसमस बमबारी ऑपरेशन: यह ऑपरेशन 18-29 दिसंबर, 1972 तक चलाया गया था। यह बी-52 बमवर्षकों द्वारा हनोई और हैफोंग शहरों पर बमबारी थी।
1973: ऑपरेशन निकेल ग्रास, योम किप्पुर युद्ध के दौरान इसराईल को हथियार और आपूर्ति पहुंचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया एक रणनीतिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन।
1974: साइप्रस से निकासी: संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना बलों ने साइप्रस पर तुर्की के आक्रमण के दौरान अमेरिकी नागरिकों को निकाला।
1975: वियतनाम से निकासी: ऑपरेशन फ़्रीक्वेंट विंड, 3 अप्रैल 1975 को, राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने बताया कि वियतनाम से शरणार्थियों और अमेरिकी नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और मरीन को भेजा गया था।
1975: कंबोडिया से निकासी: ऑपरेशन ईगल पुल, 12 अप्रैल, 1975 को, राष्ट्रपति फोर्ड ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य बलों को कंबोडिया से अमेरिकी नागरिकों की योजनाबद्ध निकासी के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया था।
1975: दक्षिण वियतनाम: 30 अप्रैल, 1975 को, राष्ट्रपति फोर्ड ने बताया कि 70 निकासी हेलीकाप्टरों और 865 नौसैनिकों की एक सेना ने लगभग 1,400 अमेरिकी नागरिकों और 5,500 तीसरे देश के नागरिकों और दक्षिण वियतनामी लोगों को अमेरिकी दूतावास, साइगॉन और टैन सोन नहट हवाई अड्डे के आसपास के लैंडिंग क्षेत्रों से निकाला था।
1975: कंबोडिया: मायागुएज़ घटना, 15 मई, 1975 को, राष्ट्रपति फोर्ड ने बताया कि उन्होंने सैन्य बलों को एसएस मायागुएज़, एक व्यापारी जहाज़ को वापस लेने का आदेश दिया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय जल में कंपूचियन रिवोल्यूशनरी आर्मी के नौसैनिक गश्ती नौकाओं से ज़ब्त कर लिया गया था और पास के एक द्वीप पर जाने के लिए मजबूर किया गया था।
1976: लेबनान: 22 और 23 जुलाई 1976 को, पांच अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों के हेलीकॉप्टरों ने लेबनानी गुटों के बीच लड़ाई के दौरान लेबनान से लगभग 250 अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों को निकाला, क्योंकि शत्रुता के कारण एक भूमिगत काफिले की निकासी अवरुद्ध हो गई थी।
1976: कोरिया: कोरियाई असैन्यीकृत क्षेत्र में एक पेड़ काटते समय उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा दो अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद कोरिया में अतिरिक्त बल भेजे गए।
1978: ज़ैरे (कांगो): 19 मई से जून के अंत तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ज़ैरे में बेल्जियम और फ्रांसीसी बचाव कार्यों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए सैन्य परिवहन विमान का उपयोग किया।
1980: ईरान: ऑपरेशन ईगल क्लॉ, 26 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रपति कार्टर ने ईरान में अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के असफल प्रयास में छह अमेरिकी परिवहन विमानों और आठ हेलीकॉप्टरों के उपयोग की सूचना दी।
1980: अमेरिकी सेना और वायु सेना की इकाइयां "ऑपरेशन ब्राइट स्टार" के हिस्से के रूप में सितंबर में सिनाई पहुंचीं। वे 1979 में हस्ताक्षरित कैंप डेविड शांति समझौते के हिस्से के रूप में मिस्र के सशस्त्र बलों के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए वहां पहुंचे। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में पहला अमेरिकी सैन्य बल था।
1981: अल साल्वाडोर: अल साल्वाडोर की सरकार के ख़िलाफ़ गुरिल्ला हमले के बाद, अतिरिक्त अमेरिकी सैन्य सलाहकारों को अल साल्वाडोर भेजा गया, जिससे कुल संख्या लगभग 55 हो गई, ताकि विद्रोह विरोधी सरकारी बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिल सके।
1981: लीबिया: सिदरा की खाड़ी की पहली घटना, 19 अगस्त 1981 को, वाहक यूएसएस निमित्ज़ पर आधारित अमेरिकी विमानों ने सिदरा की खाड़ी के ऊपर दो लीबियाई जेटों को मार गिराया, क्योंकि लीबिया के एक जेट ने एक मिसाइल दागी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने समय-समय पर सिदरा की खाड़ी में नेविगेशन अभ्यास की स्वतंत्रता का आयोजन किया। पालांकि वह लीबिया क्षेत्रीय जल क्षेत्र था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका उसे अंतरराष्ट्रीय जल-क्षेत्र बताता था।
1982: सिनाई: 19 मार्च 1982 को, राष्ट्रपति रीगन ने सिनाई प्रायद्वीप में बहुराष्ट्रीय बल और पर्यवेक्षकों में भाग लेने के लिए सैन्य कर्मियों और उपकरणों की तैनाती की सूचना दी। भागीदारी को बहुराष्ट्रीय बल और पर्यवेक्षक संकल्प, सार्वजनिक कानून 97-132 द्वारा अधिकृत किया गया था।
1982: लेबनान: लेबनान में बहुराष्ट्रीय बल, 21 अगस्त 1982 को, राष्ट्रपति रीगन ने बेरूत से फ़िलिस्तीन मुक्ति बल के सदस्यों की वापसी में सहायता के लिए बहुराष्ट्रीय बल में सेवा करने के लिए 800 नौसैनिकों को भेजने की सूचना दी। नौसैनिक 20 सितम्बर 1982 को चले गए।
1982-1983: लेबनान: 29 सितंबर, 1982 को, राष्ट्रपति रीगन ने लेबनानी सरकार की संप्रभुता की बहाली की सुविधा के लिए एक अस्थायी बहुराष्ट्रीय बल में सेवा देने के लिए 1200 नौसैनिकों की तैनाती की सूचना दी। 29 सितंबर, 1983 को, कांग्रेस ने लेबनान में बहुराष्ट्रीय बल प्रस्ताव (पी।एल। 98-119) पारित किया, जिसमें अठारह महीनों तक निरंतर भागीदारी को अधिकृत किया गया।
1983: मिस्र: 18 मार्च 1983 को लीबियाई विमान द्वारा सूडान के एक शहर पर बमबारी करने और सूडान तथा मिस्र द्वारा सहायता की अपील करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिस्र के लिए एक AWACS इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमान भेजा।
1983: ग्रेनेडा: ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी, सोवियत और क्यूबा के प्रभाव के बढ़ते ख़तरे का हवाला देते हुए और तख्तापलट के बाद एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और सोवियत संघ और क्यूबा के साथ गठबंधन को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका ने ग्रेनेडा के द्वीप राष्ट्र पर आक्रमण किया।
1983-1989: होंडुरास: जुलाई 1983 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने होंडुरास में कई अभ्यास किए, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि इससे निकारागुआ के साथ संघर्ष हो सकता है। 25 मार्च, 1986 को अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टरों और चालक दल के सदस्यों ने निकारागुआ के सैनिकों को पीछे हटाने के लिए होंडुरास के सैनिकों को निकारागुआ की सीमा तक पहुंचाया।
1983: चाड: 8 अगस्त 1983 को, राष्ट्रपति रीगन ने लीबियाई और विद्रोही बलों के ख़िलाफ़ चाड की सहायता के लिए दो AWACS इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमानों और आठ F-15 लड़ाकू विमानों और जमीनी रसद सहायता बलों की तैनाती की सूचना दी।
1984: फारस की खाड़ी: 5 जून 1984 को, सऊदी अरब के जेट लड़ाकू विमानों ने, अमेरिकी AWACS इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विमान की खुफिया जानकारी की सहायता से और अमेरिकी KC-10 टैंकर द्वारा ईंधन भरते हुए, फारस की खाड़ी के एक क्षेत्र में दो ईरानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसे शिपिंग के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।
1985: इटली: 10 अक्टूबर 1985 को अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने मिस्र के एक विमान को रोका और उसे सिसिली में उतरने के लिए मजबूर किया। विमान में इतालवी क्रूज जहाज़ अकिल लॉरो के अपहरणकर्ता सवार थे जिन्होंने अपहरण के दौरान एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर दी थी।
1986: लीबिया: सिदरा की खाड़ी में कार्रवाई (1986), 26 मार्च, 1986 को, राष्ट्रपति रीगन ने 24 और 25 मार्च को रिपोर्ट दी, अमेरिकी सेना, जब सिदरा की खाड़ी के आसपास नेविगेशन अभ्यास की स्वतंत्रता में लगी हुई थी, तो उस ने लीबिया पर मिसाइलों द्वारा हमला किया।
1986: लीबिया: ऑपरेशन एल डोरैडो कैनियन, 16 अप्रैल 1986 को, राष्ट्रपति रीगन ने बताया कि अमेरिकी वायु और नौसेना बलों ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली में आतंकवादी सुविधाओं और सैन्य प्रतिष्ठानों पर बमबारी की थी।
1987: फारस की खाड़ी: 17 मई को ईरान-इराक़ युद्ध के दौरान इराकी वायु सेना के डसॉल्ट मिराज एफ1 से दागी गई दो एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइलों से यूएसएस स्टार्क पर हमला किया गया, जिसमें 37 अमेरिकी नौसेना नाविक मारे गए।
1987: फारस की खाड़ी: ऑपरेशन निम्बल आर्चर। 19 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा फारस की खाड़ी में दो ईरानी तेल प्लेटफार्मों पर हमला।
1987-1988: फारस की खाड़ी: ऑपरेशन अर्नेस्ट विल। ईरान-इराक़ युद्ध (टैंकर युद्ध चरण) के परिणामस्वरूप फारस की खाड़ी में कई सैन्य घटनाएं हुईं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी संयुक्त सैन्य बलों के संचालन में वृद्धि की और इराकी और ईरानी हमलों से बचाने के लिए फारस की खाड़ी के माध्यम से कुवैती तेल टैंकरों पर नियंत्रण पाने की नीति अपनाई। राष्ट्रपति रीगन ने बताया कि 21 सितंबर (ईरान अजर), 8 अक्टूबर और 19 अक्टूबर, 1987, और 18 अप्रैल (ऑपरेशन प्रेयरिंग मेंटिस), 3 जुलाई और 14 जुलाई, 1988 को अमेरिकी जहाज़ों पर गोलीबारी की गई या खदानों पर हमला किया गया या अन्य सैन्य कार्रवाई की गई।
1987-1988: फारस की खाड़ी: ऑपरेशन प्राइम चांस एक संयुक्त राज्य अमेरिका का विशेष ऑपरेशन कमांड ऑपरेशन था जिसका उद्देश्य ईरान-इराक़ युद्ध के दौरान अमेरिकी ध्वज वाले तेल टैंकरों को ईरानी हमले से बचाना था। यह ऑपरेशन ऑपरेशन अर्नेस्ट विल के साथ ही हुआ।
1988: फारस की खाड़ी: ऑपरेशन प्रेयरिंग मेंटिस 18 अप्रैल, 1988 को फारस की खाड़ी में ईरानी खनन और उसके बाद एक अमेरिकी युद्धपोत को हुए नुक़सान के प्रतिशोध में अमेरिकी नौसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई थी।
1988: होंडुरास: ऑपरेशन गोल्डन फीसैंट 1988 में निकारागुआ (तत्कालीन समाजवादी) की सेनाओं की धमकी भरी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप होंडुरास में अमेरिकी सैनिकों की एक आपातकालीन तैनाती थी।
1988: यूएसएस विन्सेन्स ने ईरान एयर फ़्लाइट 655 को मार गिराया।
1988: पनामा: मार्च के मध्य और अप्रैल 1988 में, पनामा में अस्थिरता की अवधि के दौरान और जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा के राज्य प्रमुख जनरल मैनुअल नोरिएगा पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ाया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने "नहर, अमेरिकी जीवन, संपत्ति और क्षेत्र में हितों की और अधिक सुरक्षा" के लिए पनामा में 1,000 सैनिक भेजे। सेना ने पनामा नहर क्षेत्र में पहले से ही 10,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों को शामिल किया।
1989: लीबिया: सिदरा की दूसरी खाड़ी घटना। 4 जनवरी 1989 को, यूएसएस जॉन एफ। कैनेडी पर आधारित दो अमेरिकी नौसेना एफ-14 विमानों ने लीबिया से लगभग 70 मील उत्तर में भूमध्य सागर के ऊपर दो लीबियाई जेट लड़ाकू विमानों को मार गिराया। अमेरिकी पायलटों ने कहा कि लीबियाई विमानों ने शत्रुतापूर्ण इरादे प्रदर्शित किए थे।
1989: पनामा: 11 मई 1989 को, जनरल नोरिएगा द्वारा पनामा चुनाव के परिणामों की उपेक्षा के जवाब में, राष्ट्रपति बुश ने क्षेत्र में पहले से मौजूद अनुमानित 1,000 अमेरिकी बलों को बढ़ाने के लिए लगभग 1,900 सैनिकों की एक ब्रिगेड-आकार की सेना का आदेश दिया।
1989: कोलंबिया, बोलीविया और पेरू: ड्रग्स पर युद्ध में एंडियन पहल, 15 सितंबर 1989 को, राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि कोलंबिया, बोलीविया और पेरू के एंडियन देशों को अवैध ड्रग उत्पादकों और तस्करों से निपटने में मदद करने के लिए सैन्य और कानून प्रवर्तन सहायता भेजी जाएगी। सितंबर के मध्य तक सैन्य उपकरणों के उपयोग में परिवहन और प्रशिक्षण के संबंध में कोलंबिया में 50-100 अमेरिकी सैन्य सलाहकार थे, साथ ही तीन देशों में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2-12 व्यक्तियों की सात विशेष बल टीमें थीं।
1989: फिलीपींस: ऑपरेशन क्लासिक रिज़ॉल्व, 2 दिसंबर 1989 को, राष्ट्रपति बुश ने बताया कि 1 दिसंबर को, लूज़ोन में क्लार्क एयर बेस से वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए एक्विनो सरकार की सहायता की थी। इसके अलावा, मनीला में संयुक्त राज्य दूतावास की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना बेस सुबिक बे से 100 नौसैनिकों को भेजा गया था।
1989-1990: पनामा: पनामा पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आक्रमण और ऑपरेशन जस्ट कॉज़, 21 दिसंबर 1989 को, राष्ट्रपति बुश ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और जनरल नोरिएगा को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों को पनामा में जाने का आदेश दिया था। इस में लगभग 200 पनामा नागरिकों को मार दिया गया और पनामा के राज्य प्रमुख जनरल मैनुएल नोरिएगा को पकड़ कर अमेरिका ले जाया गया।
1990: लाइबेरिया: 6 अगस्त 1990 को, राष्ट्रपति बुश ने बताया कि मोनरोविया में अमेरिकी दूतावास को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रबलित राइफल कंपनी भेजी गई थी, और हेलीकॉप्टर टीमों ने लाइबेरिया से अमेरिकी नागरिकों को निकाला ।
1990: सऊदी अरब: 9 अगस्त 1990 को, राष्ट्रपति बुश ने बताया कि उन्होंने 2 अगस्त को इराक़ द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद सऊदी अरब की रक्षा में मदद करने के लिए फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सशस्त्र बलों के पर्याप्त तत्वों की अग्रिम तैनाती का आदेश देकर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया है। 16 नवंबर 1990 को, उन्होंने पर्याप्त आक्रामक सैन्य विकल्प सुनिश्चित करने के लिए बलों के निरंतर निर्माण की सूचना दी।
1991: इराक़: ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, 17 जनवरी 1991 से 11 अप्रैल 1991 तक मित्र राष्ट्रों की ओर से आक्रामक लैंडिंग।ऑपरेशन डेजर्ट सेबर, 24-27 फरवरी, 1991 तक मित्र देशों का ज़मीनी आक्रमण।
1991-1996: इराक़: 1991 के विद्रोह के दौरान उत्तरी इराक़ में अपने घरों से भाग रहे कुर्दों के लिए तुर्की में स्थित एक छोटी सहयोगी जमीनी सेना द्वारा ऑपरेशन प्रोवाइड कम्फर्ट, मानवीय राहत और सैन्य सुरक्षा प्रदान की गई, जो अप्रैल 1991 में शुरू हुई।
1991: इराक़: 17 मई 1991 को, राष्ट्रपति बुश ने कहा कि कुर्द लोगों के इराकी दमन के कारण आपातकालीन राहत उद्देश्यों के लिए उत्तरी इराक़ में अमेरिकी सेना की सीमित तैनाती आवश्यक हो गई थी।
1991: ज़ैरे: 25-27 सितंबर, 1991 को, किंशासा में बड़े पैमाने पर लूटपाट और दंगे भड़कने के बाद, वायु सेना सी-141 ने 100 बेल्जियम सैनिकों और उपकरणों को किंशासा पहुंचाया। अमेरिकी विमान 300 फ्रांसीसी सैनिकों को भी मध्य अफ़्रीकी गणराज्य में ले गए और निकाले गए अमेरिकी नागरिकों को ले गए।
1992: सिएरा लियोन: ऑपरेशन सिल्वर एनविल, 29 अप्रैल के तख्तापलट के बाद, जिसने राष्ट्रपति जोसेफ सैदु मोमोह को उखाड़ फेंका, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड (USEUCM) के संयुक्त विशेष अभियान टास्क फोर्स ने 3 मई को 438 लोगों (42 तीसरे देश के नागरिकों सहित) को निकाला। दो एयर मोबिलिटी कमांड (AMC) C-141 ने फ्रीटाउन, सिएरा लियोन से 136 लोगों को जर्मनी के राइन-मेन एयर बेस और नौ C-130 के लिए उड़ान भरी। उड़ानें अन्य 302 लोगों को डकार, सेनेगल ले गईं।
1992-1996: बोस्निया और हर्जेगोविना: ऑपरेशन प्रोवाइड प्रॉमिस 2 जुलाई 1992 से 9 जनवरी 1996 तक यूगोस्लाव युद्धों के दौरान बोस्निया और हर्जेगोविना में एक मानवीय राहत अभियान था, जिसने इसे इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मानवीय एयरलिफ्ट बना दिया।
1992: कुवैत: 3 अगस्त 1992 को, इराक़ द्वारा संयुक्तराष्ट्र की बनाई हुई नई सीमा को मान्यता देने से इनकार करने और संयुक्तराष्ट्र निरीक्षण टीमों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत में सैन्य अभ्यास की एक श्रृंखला शुरू की।
1992-2003: इराक़: इराकी नो-फ्लाई जोन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और उसके खाड़ी युद्ध सहयोगियों ने संप्रभु इराकी हवाई क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर "नो-फ्लाई जोन" घोषित और लागू किया, दक्षिणी इराक़ और उत्तरी इराक़ में जोनों में इराकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया, हवाई टोही आयोजित की, और संयुक्तराष्ट्र के आदेश के हिस्से के रूप में इराकी वायु-रक्षा प्रणालियों पर कई विशिष्ट हमले किए। अक्सर, इराकी सेनाएं नो-फ्लाई जोन में गश्त कर रहे अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों पर गोलीबारी करके पूरे एक दशक तक जारी रहीं।
1993-1995: बोस्निया: ऑपरेशन डेनी फ़्लाइट, 12 अप्रैल 1993 को, संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 816 के पारित होने के जवाब में, अमेरिका और नाटो ने बोस्नियाई हवाई क्षेत्र पर नो-फ़्लाई ज़ोन लागू किया, सभी अनधिकृत उड़ानों पर रोक लगा दी और "[नो-फ़्लाई ज़ोन प्रतिबंधों] का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की अनुमति दी।"
1993: सोमालिया: मोगादिशु की लड़ाई, या मोगादिशु की पहली लड़ाई, ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट का परिणाम। अक्टूबर 3-4, 1993, टास्क फोर्स रेंजर, जो बड़े पैमाने पर 75वीं रेंजर रेजिमेंट और डेल्टा फोर्स से बनी थी, ने दो उच्च रैंकिंग वाले सोमाली राष्ट्रीय सेना नायकों को पकड़ने के लिए मोगादिशू के रिहाइशी इलाक़ों में प्रवेश किया। दो अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक्स को मार गिराया गया, 18 अमेरिकी कार्रवाई में मारे गए, अन्य 73 घायल हो गए, और 1 को पकड़ लिया गया। लड़ाई की घटनाओं को ब्लैक हॉक डाउन पुस्तक में संकलित किया गया था, जिसे बाद में उसी नाम की फिल्म में रूपांतरित किया गया।
1993: मैसेडोनिया: 9 जुलाई 1993 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने पूर्व यूगोस्लाविया के क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा बल में भाग लेने के लिए मैसेडोनिया गणराज्य में 350 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की सूचना दी।
1994: बोस्निया: बंजा लुका घटना, नाटो पहली युद्ध स्थिति में शामिल हो गया जब नाटो अमेरिकी वायु सेना एफ -16 जेट विमानों ने संयुक्तराष्ट्र-शासित नो-फ्लाई ज़ोन का उल्लंघन करने के लिए छह बोस्नियाई सर्ब जे -21 जस्त्रेब (J-21 Jastreb) सिंगल-सीट लाइट अटैक जेट में से चार को मार गिराया।
1994-1995: हैती: ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी, अमेरिकी जहाज़ों ने हैती के ख़िलाफ़ प्रतिबंध शुरू कर दिया था। एक बड़े तख्तापलट के बाद 1991 में सत्ता में आए सैन्य शासन से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हैती के राष्ट्रपति जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड को बहाल करने के लिए बाद में 20,000 अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों को हैती में तैनात किया गया ।
1994: मैसेडोनिया: 19 अप्रैल, 1994 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने बताया कि मैसेडोनिया में अमेरिकी दल में 200 कर्मियों की एक प्रबलित कंपनी की वृद्धि की गई है।
1994: कुवैत: ऑपरेशन विजिलेंट वॉरियर अक्टूबर 1994 में शुरू हुआ जब इराकी रिपब्लिकन गार्ड डिवीजनों ने कुवैती सीमा के पास इराक़ के दक्षिण में फिर से स्थान बनाना शुरू किया। अमेरिकी सेना ने खाड़ी में सेना की आवाजाही के साथ जवाबी कार्रवाई की - ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के बाद सबसे बड़ा। ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर 22 दिसंबर 1994 को समाप्त हो गया।
1995: बोस्निया: ऑपरेशन डेलीब्रेट फोर्स, 30 अगस्त 1995 को, अमेरिका और नाटो विमानों ने साराजेवो बाजार पर बोस्नियाई सर्ब मोर्टार हमले के जवाब में बोस्नियाई सर्ब सेना का एक बड़ा बमबारी अभियान शुरू किया, जिसमें 28 अगस्त, 1995 को 37 लोग मारे गए। यह ऑपरेशन 20 सितंबर, 1995 तक चला। सर्ब पदों के ख़िलाफ़ मुस्लिम और क्रोएशियाई सेना की संयुक्त सहयोगी जमीनी सेना के साथ हवाई अभियान दिसंबर 1995 में युद्धरत गुटों के हस्ताक्षर के साथ डेटन समझौता हुआ। ऑपरेशन ज्वाइंट एंडेवर के हिस्से के रूप में, अमेरिका और नाटो ने डेटन समझौते को बनाए रखने के लिए कार्यान्वयन बल (आईएफओआर) के शांति सैनिकों को बोस्निया भेजा।
1996: मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, ऑपरेशन त्वरित प्रतिक्रिया: 23 मई 1996 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने "निजी अमेरिकी नागरिकों और कुछ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों" के देश से निकासी के लिए, और "बंगुई में अमेरिकी दूतावास के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा" प्रदान करने के लिए, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य के बांगुई में अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती की सूचना दी। दूतावास में और 190-208 अमेरिकियों सहित 448 लोगों को निकाला गया। आखिरी नौसैनिक 22 जून को बांगुई से रवाना हुए।
1996: कुवैत: ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, इराकी सेना के हमलों के ख़िलाफ़ कुर्द आबादी की रक्षा के लिए उत्तर में अमेरिकी हवाई हमले।
1996: बोस्निया: ऑपरेशन ज्वाइंट गार्ड, 21 दिसंबर 1996 को, अमेरिका और नाटो ने डेटन समझौते के तहत शांति लागू करने के लिए आईएफओआर के स्थान पर एसएफओआर शांति सैनिकों की स्थापना की।
1997: अल्बानिया: ऑपरेशन सिल्वर वेक, 13 मार्च 1997 को, तिराना, अल्बानिया से कुछ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और निजी अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों का इस्तेमाल किया गया था।
1997: कांगो और गैबॉन: 27 मार्च, 1997 को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने 25 मार्च, 1997 को रिपोर्ट दी, कि बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी आवश्यक निकासी अभियान के लिए उपलब्ध रहने के लिए कांगो और गैबॉन में अमेरिकी सैन्य कर्मियों का एक अतिरिक्त निकासी बल तैनात किया गया ।
1997: सिएरा लियोन: 29 और 30 मई, 1997 को, कुछ अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और निजी अमेरिकी नागरिकों की निकासी की तैयारी और कार्य करने के लिए, अमेरिकी सैन्य कर्मियों को फ़्रीटाउन, सिएरा लियोन में तैनात किया गया था।
1997: कंबोडिया: 11 जुलाई 1997 को, कंबोडिया में घरेलू संघर्ष की अवधि के दौरान अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में, संभावित निकासी के लिए लगभग 550 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की एक टास्क फोर्स को थाईलैंड के उटापाओ एयर बेस पर तैनात किया गया था।
1998: इराक़: ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, अमेरिकी और ब्रिटिश सेना ने 16-19 दिसंबर, 1998 तक इराकी ठिकानों पर चार दिवसीय बमबारी अभियान चलाया।
1998–1999: केन्या और तंजानिया: केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी से संबंधित चिकित्सा और आपदा सहायता के समन्वय के लिए अमेरिकी सैन्य कर्मियों को नैरोबी, केन्या में तैनात किया गया था।
1998: अफ़ग़ानिस्तान और सूडान: ऑपरेशन इनफिनिट रीच। 20 अगस्त को, राष्ट्रपति क्लिंटन ने अफ़ग़ानिस्तान में दो संदिग्ध आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और सूडान में एक संदिग्ध रासायनिक कारखाने के ख़िलाफ़ क्रूज मिसाइल हमले का आदेश दिया।
1998: लाइबेरिया: 27 सितंबर 1998 को, अमेरिका ने मोनरोविया में अमेरिकी दूतावास में सुरक्षा बल बढ़ाने के लिए 30 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की एक स्टैंड-बाय प्रतिक्रिया और निकासी बल तैनात किया।
1999-2001: पूर्वी तिमोर: पूर्वी तिमोर में शांति बहाली के नाम पर पूर्वी तिमोर के लिए संयुक्तराष्ट्र द्वारा अधिदेशित अंतर्राष्ट्रीय बल के साथ सीमित संख्या में अमेरिकी सैन्य बल तैनात किए गए।
1999: सर्बिया: ऑपरेशन अलाइड फोर्स: कोसोवो में जातीय अल्बानियाई लोगों के ख़िलाफ़ दमन को समाप्त करने के लिए सर्बियाई राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविक के इनकार के कारण कोसोवो युद्ध के दौरान 24 मार्च 1999 को अमेरिका और नाटो विमानों ने कोसोवो में सर्बिया और सर्ब पदों पर बड़ी बमबारी शुरू कर दी। यह ऑपरेशन 10 जून 1999 को समाप्त हुआ, जब मिलोसेविक अपने सैनिकों को कोसोवो से बाहर निकालने के लिए सहमत हो गया। कोसोवो की स्थिति के जवाब में, नाटो ने यूएनएससी संकल्प 1244 के तहत शांति सुनिश्चित करने के लिए केएफओआर शांति सैनिकों को भेजा।
2000: सिएरा लियोन: 12 मई 2000 को, जरूरत पड़ने पर उस देश से निकासी कार्यों का समर्थन करने के लिए अमेरिकी नौसेना के एक गश्ती जहाज़ को सिएरा लियोन में तैनात किया गया।
2000: नाइजीरिया: देश में एक प्रशिक्षण मिशन का नेतृत्व करने के लिए विशेष बल के सैनिकों को नाइजीरिया भेजा गया।
2000: यमन: 12 अक्टूबर 2000 को, यमन के अदन बंदरगाह पर यूएसएस कोल के हमले के बाद, सैन्य कर्मियों को अदन में तैनात किया गया था।
2000: पूर्वी तिमोर: 25 फरवरी 2000 को, पूर्वी तिमोर में संयुक्तराष्ट्र संक्रमणकालीन प्रशासन (UNTAET) का समर्थन करने के लिए छोटी संख्या में अमेरिकी सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया।
2001: 1 अप्रैल 2001 को, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी EP-3E ARIES II सिग्नल निगरानी विमान और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) J-8II इंटरसेप्टर फाइटर जेट के बीच हवा में टक्कर के परिणामस्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच एक अंतरराष्ट्रीय विवाद पैदा हो गया, जिसे हैनान द्वीप घटना कहा जाता है।
2001-2021: अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध: आतंक के ख़िलाफ़ युद्ध ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम से शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को, 9/11 के हमलों के जवाब में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण किया और "अफ़ग़ानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के नाम पर विध्वंस शुरू किया।"
2002: यमन: 3 नवंबर 2002 को, एक अमेरिकी एमक्यू-1 प्रीडेटर ने यमन में एक कार पर हेलफायर मिसाइल दागी, जिसमें कथित अल-क़ायदा नेता कायद सलीम सिनान अल-हरेथी की मौत हो गई, जिसे कथित रूप से यूएसएस कोल बमबारी के लिए ज़िम्मेदार माना जाता था।
2002: फिलीपींस: ओईएफ-फिलीपींस, जनवरी तक, अमेरिकी "लड़ाकू-सुसज्जित और लड़ाकू सहायता बल" को फिलीपीन सशस्त्र बलों को उनकी "आतंकवाद विरोधी क्षमताओं" को बढ़ाने में प्रशिक्षित करने, सहायता करने और सलाह देने के लिए फिलीपींस में तैनात किया गया है।
2002: कोटे डी आइवर: 25 सितंबर, 2002 को, कोटे डी आइवर में विद्रोह के जवाब में, अमेरिकी सैन्यकर्मी बौआके से अमेरिकी नागरिकों की निकासी में सहायता करने के लिए कोटे डी आइवर में गए।
2003-2011: इराक़ में युद्ध: ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, 20 मार्च 2003, संयुक्त राज्य अमेरिका एक गठबंधन का नेतृत्व करता है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड शामिल हैं, जो इराक़ पर आक्रमण करने के लिए हैं, जिसका घोषित लक्ष्य "खाड़ी क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की खोज में इराक़ को निरस्त्र करना है।" हालांकि अघोषित लक्ष्य इराक़ के प्राकृतिक संसाधनों पर क़ब्ज़ा था।
2003: लाइबेरिया: दूसरा लाइबेरिया गृह युद्ध, 9 जून 2003 को, राष्ट्रपति बुश ने बताया कि 8 जून को उन्होंने नौआकचॉट, मॉरिटानिया में अमेरिकी दूतावास को सुरक्षित करने में मदद करने और लाइबेरिया या मॉरिटानिया से किसी भी आवश्यक निकासी में सहायता के लिए लगभग 35 अमेरिकी नौसैनिकों को लाइबेरिया के मोनरोविया में भेजा।
2003: जॉर्जिया और जिबूती: "अमेरिकी युद्ध से सुसज्जित और सहायक बल" को उनकी "आतंकवाद विरोधी क्षमताओं" को बढ़ाने में मदद करने के लिए जॉर्जिया और जिबूती में तैनात किया गया।
2004: हैती: 2004 में हैती में तख्तापलट हुआ, अमेरिका ने सबसे पहले वहां अमेरिकी दूतावास के सुरक्षा बलों को बढ़ाने और अमेरिकी नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए 55 लड़ाकू सुसज्जित सैन्य कर्मियों को भेजा। बाद में संयुक्तराष्ट्र बहुराष्ट्रीय अंतरिम बल, MINUSTAH के लिए रास्ता तैयार करने के लिए 200 अतिरिक्त अमेरिकी युद्ध-सुसज्जित सैन्य कर्मियों को भेजा गया।
2004: आतंक के विरुद्ध युद्ध: जॉर्जिया, जिबूती, केन्या, इथियोपिया, यमन और इरिट्रिया में अमेरिकी आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ चल रही थीं।
2004-वर्तमान: अमेरिका ने उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में युद्ध में सहायता के लिए ड्रोन हमले तैनात किए।
2005-2006: पाकिस्तान: राष्ट्रपति बुश ने बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित पाकिस्तान के कश्मीर पर्वत श्रृंखला के दूर-दराज के गांवों में मानवीय राहत प्रदान करने के लिए अमेरिकी सेना के हवाई घुड़सवार ब्रिगेड के सैनिकों को तैनात किया।
2005-2008: ऑपरेशन विलिंग स्पिरिट, कोलंबिया - एफएआरसी द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी बंधकों को बचाया गया।
2006: लेबनान: 24वीं समुद्री अभियान इकाई का हिस्सा ने इसराईल द्वारा संभावित जमीनी आक्रमण और हिजबुल्लाह और इसराईली सेना के बीच जारी लड़ाई के कारण देश छोड़ने के इच्छुक अमेरिकी नागरिकों की निकासी शुरू की।
2007 - मोगादिशु मुठभेड़, 29 अक्टूबर 2007 को सोमाली समुद्री लुटेरों ने एक उत्तर कोरियाई व्यापारी जहाज़ पर चढ़कर हमला कर दिया। पास से गुजर रहे अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों और एक हेलीकॉप्टर ने, जो उस समय गश्त कर रहे थे, हमले का जवाब दिया। एक बार जब जहाज़ को समुद्री डाकुओं से मुक्त कर दिया गया, तो अमेरिकी बलों को जहाज़ पर चढ़ने और घायल चालक दल की सहायता करने और जीवित समुद्री डाकुओं को संभालने की अनुमति दी गई।
2007: सोमालिया: रास कंबोनी की लड़ाई, 8 जनवरी 2007 को, जबकि इस्लामिक कोर्ट यूनियन और ट्रांजिशनल फेडरल सरकार के बीच संघर्ष जारी है, एक एसी-130 गनशिप ने दक्षिणी सोमालिया में रास कंबोनी के पास बदमाडो द्वीप पर अन्य इस्लामी लड़ाकों के साथ एक संदिग्ध अल-क़ायदा ऑपरेटिव पर हवाई हमला किया।
2010-वर्तमान: यमन में अल-क़ायदा विद्रोह: अमेरिका यमन में संदिग्ध अल-क़ायदा, अल-शबाब और आईएसआईएस ठिकानों पर ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला।
2010-2011: ऑपरेशन न्यू डॉन, 17 फरवरी 2010 को, अमेरिकी रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने घोषणा की कि 1 सितंबर 2010 से, "ऑपरेशन इराकी फ्रीडम" नाम को "ऑपरेशन न्यू डॉन" से बदल दिया जाएगा। यह अमेरिकी सैनिकों की संख्या में 50,000 की कमी के साथ मेल खाता है।
2011: 2011 लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप: ऑपरेशन ओडिसी डॉन, संयुक्त राज्य अमेरिका और गठबंधन ने लीबियाई बलों पर बमबारी के साथ संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1973 को लागू किया।
2011: ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य बलों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराने का ड्रामा रचा।
2011: कथित अल-शबाब आतंकवादियों केबहाने सोमालिया पर ड्रोन हमले शुरू हुए। यह छठा देश है जहां इस तरह के हमले किए गए। जिसमें अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, इराक़, यमन और लीबिया शामिल हैं।
2011-वर्तमान: युगांडा: अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों को सलाहकार के रूप में युगांडा भेजा गया।
2012: जॉर्डन: सीरिया की सीमाओं के भीतर सीरियाई गृह युद्ध को रोकने के बहाने 150 अमेरिकी सैनिकों को जॉर्डन में तैनात किया गया।
2012: तुर्की: सीरिया से किसी भी मिसाइल हमले को रोकने के लिए 400 सैनिक और पैट्रियट मिसाइलों की दो बैटरियां तुर्की भेजी गईं।
2012: चाड: शहर की ओर विद्रोहियों के बढ़ने के मद्देनज़र पड़ोसी मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई से अमेरिकी नागरिकों और दूतावास कर्मियों को निकालने में मदद करने के लिए 50 अमेरिकी सैनिकों को अफ्रीकी देश चाड में तैनात किया गया है।
2013: माली: अमेरिकी सेना ने हवाई ईंधन भरने और परिवहन विमान के साथ ऑपरेशन सर्वल में फ्रांसीसी की सहायता की।
2013: सोमालिया: अमेरिकी वायु सेना के विमानों ने बुलो मारेर बंधक बचाव प्रयास में फ्रांसीसियों का सहयोग किया। हालाँकि, उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया।
2013: 2013 कोरियाई संकट
2013: नेवी सील्स ने सोमालिया में छापा मारा और कथित रूप से अल-शबाब के एक वरिष्ठ अधिकारी को मार डाला, साथ ही एक और छापा लीबिया के त्रिपोली में हुआ, जहां विशेष अभियान बलों ने अबू अनस अल लिबी (जिसे अनस अल-लिबी के नाम से भी जाना जाता है) को पकड़ लिया।
2014-वर्तमान: युगांडा: वी-22 ऑस्प्रे, एमसी-130एस, केसी-135एस और अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को जोसेफ कोनी की खोज में अफ्रीकी बलों की मदद जारी रखने के लिए युगांडा भेजा गया है।
2014–वर्तमान: इराक़ में अमेरिकी हस्तक्षेप: इराक़ में अमेरिकी संपत्ति की रक्षा करने और इराकी और कुर्द लड़ाकों से निपटने के लिए सैकड़ों अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए। अमेरिकी वायु सेना ने एक मानवीय हवाई हमला किया और अमेरिकी नौसेना ने पूरे उत्तरी इराक़ में इस्लामिक स्टेट-गठबंधन बलों के विरोध के नाम पर हवाई हमलों की बरसात शुरू कर दी।
2014: 2014 सीरिया में अमेरिकी बचाव अभियान: अमेरिका ने आईएसआईएल (Islamic State in Iraq and the Levant) द्वारा बंधक बनाए गए जेम्स फोले और अन्य को बचाने का प्रयास किया। "ओसामा बिन लादेन शिविर" के नाम से जाने जाने वाले आईएसआईएल सैन्य अड्डे पर हवाई हमले किए गए। इस बीच, बमबारी के बाद, डेल्टा टीमों ने आईएसआईएल की हाई वैल्यूड जेल के पास पैराशूट से उड़ान भरी। किसी भी लक्ष्य को भागने से रोकने के लिए मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था। जब कोई बंधक नहीं मिला तो अमेरिकी सैनिकों ने घर-घर तलाशी शुरू कर दी और बहुत तबाही मचाई। बंधक कहीं नहीं मिले और मिशन विफल रहा। आईएसआईएल आतंकवादी बताकर कम से कम 5 लोगों को मार डाला गया, 1 अमेरिकी सैनिक घायल हउआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ऑपरेशन में जॉर्डन की भूमिका थी और जॉर्डन का भी एक सैनिक घायल हुआ।
2014-वर्तमान: सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाला हस्तक्षेप: अमेरिकी विमान ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट, अल-क़ायदा, अल-नुसरा फ्रंट, खुरासान और इसी तरह के झूठे सच्चे कथित आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारी का बहाना बनाकर सीरिया के कई शहरों को खंडहर बना दिया गया।
2014-वर्तमान: इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड द लेवेंट के ख़िलाफ़ हस्तक्षेप: सीरियाई स्थानीय बलों और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने इराक़ और सीरिया में आईएसआईएल और अल-नुसरा फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू की।
2014: 2014 अल-क़ायदा के ख़िलाफ़ यमन बंधक बचाव अभियान: 25 नवंबर को, अमेरिकी नौसेना सील और यमनी विशेष बलों ने अल-क़ायदा द्वारा रखे गए आठ बंधकों को बचाने के प्रयास में यमन में एक अभियान शुरू किया। हालाँकि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन किसी भी अमेरिकी बंधक को सुरक्षित नहीं किया गया। पहले प्रयास में, छह यमनियों, एक सऊदी अरब और एक इथियोपियाई को बचाया गया। 4 दिसंबर 2014 को, अरब प्रायद्वीप में अल-क़ायदा (एक्यूएपी) ने धमकी दी कि अगर अमेरिका अनिर्दिष्ट आदेशों में विफल रहा तो सौमर्स को मार डाला जाएगा। AQAP ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने एक और बचाव अभियान का प्रयास किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। 6 दिसंबर को दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। परिसर में 40 अमेरिकी सील और 30 यमनी सैनिक तैनात किए गए थे। जहां शेष बंधकों (सौमर्स और कोर्की) को रखा गया था, वहां अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश करने से पहले 10 मिनट तक गोलीबारी हुई। वे जीवित थे, लेकिन बुरी तरह घायल थे। साइट से दूर उड़ते समय हवा में ही सर्जरी की गई। कॉर्की की उड़ान के दौरान मृत्यु हो गई, और सौमर्स की यूएसएस माकिन द्वीप पर उतरने के बाद मृत्यु हो गई। कोई भी अमेरिकी सैनिक मारा/घायल नहीं हुआ, हालाँकि एक यमन सैनिक घायल हो गया।
2015: 30 अप्रैल, 2015, ईरान द्वारा एक वाणिज्यिक जहाज़, एमवी मार्सक टाइग्रिस को ज़ब्त करने के बाद जहाज़ों को ढाल देने के लिए अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ भेजे। ईरान और मेर्स्क के बीच एक दशक से चल रहे कानूनी विवाद के तहत, ईरान ने बो पर गोलियां चलाईं और मार्शल द्वीप समूह में पंजीकृत जहाज़ को ज़ब्त कर लिया।
2015-वर्तमान: अक्टूबर 2015 की शुरुआत में, अमेरिकी सेना ने कैमरून सरकार की मंजूरी के साथ, कैमरून में 300 सैनिकों को तैनात किया; उनका प्राथमिक मिशन स्थानीय बलों को खुफिया सहायता प्रदान करने के साथ-साथ टोही उड़ानें संचालित करना है।
2017: 2017 शायरात मिसाइल हमला: इदलिब के दक्षिण-पश्चिम में नागरिकों के ख़िलाफ़ रासायनिक हथियारों के हमले के जवाब में भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों से लॉन्च की गई टॉमहॉक मिसाइलों ने होम्स गवर्नरेट में एक सीरियाई एयरबेस पर हमला किया। सात लोग मारे गए और नौ घायल हो गए।
2018: अप्रैल 2018 में नागरिकों के ख़िलाफ़ डौमा रासायनिक हमले के जवाब में दमिश्क और होम्स के पास सैन्य ठिकानों पर अमेरिका और सहयोगियों द्वारा मिसाइल हमले शुरू किए गए।
2019: ऑपरेशन सेंटिनल: अमेरिकी सेंट्रल कमांड नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मध्य पूर्व में प्रमुख जलमार्गों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री प्रयास विकसित किया गया।
2020: बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले का जवाब। ईरान समर्थक कताएब हिजबुल्लाह के हमले के लिए अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बाद 31 दिसंबर, 2019 को बगदाद में अमेरिकी दूतावास की घेराबंदी कर दी गई, जिसमें चार सेवा सदस्य घायल हो गए और एक नागरिक ठेकेदार मारा गया। जवाब में, दूतावास की सुरक्षा और निगरानी के लिए तुरंत कुवैत से नौसैनिकों और विमानों को भेजा गया। 2 जनवरी, 2020 को, अमेरिका ने एक काफिले पर हवाई हमला किया, जिसमें ईरानी कुद्स फोर्स के मेजर-जनरल कासिम सुलैमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू महदी अल-मुहंदिस की मौत हो गई। इस क्षेत्र में अतिरिक्त 4,000 अमेरिकी सैनिक भेजे गए, जिनमें 82वें एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 750 सैनिक भी शामिल थे। 6 मई, 2020 को पेंटागन द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में, यह उद्धृत किया गया कि 2019 में इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, सोमालिया और सीरिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के हिस्से के रूप में लगभग 132 नागरिक मारे गए हैं। रक्षा विभाग (डीओडी) ने कहा कि क्रमशः लीबिया और यमन गृहयुद्ध में अमेरिकी सैन्य अभियानों के तहत कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ।
2021: फरवरी 2021 सीरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई हमला: 25 फरवरी, 2021 को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने इराक़ में अमेरिका और गठबंधन बलों के ख़िलाफ़ हाल के हमलों के जवाब में पूर्वी सीरिया में सीमा पार से सक्रिय ईरानी समर्थित इराकी मिलिशिया द्वारा क़ब्ज़ा कर लिया गया एक स्थल पर हवाई हमला किया।
2021: 27 जून, 2021, अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में अमेरिकी बलों और सुविधाओं पर ड्रोन हमलों के जवाब में इराक़-सीरिया सीमा के दोनों किनारों पर ईरानी समर्थित मिलिशिया पर हवाई हमले किए।
2021: सोमालिया में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप (2007-वर्तमान): 20 जुलाई, 2021, सोमालिया में अल-शबाब आतंकवादियों पर अमेरिकी सैन्य हवाई हमले किए गए, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और जनवरी 2021 में राष्ट्रपति जो बाईडेन के पदभार संभालने के बाद यह अपनी तरह का पहला हमला था। 22 जुलाई, 2021 को अमेरिकी वायु सेना द्वारा अल-शबाब आतंकवादियों के ख़िलाफ़ और हवाई हमले किए गए।
2021: 2021 अफ़ग़ानिस्तान से निकासी: 2021 में काबुल के तालिबान के हाथों में पड़ने के बाद देश से नागरिकों और अफ़ग़ान भागीदारों को निकालने के लिए नाटो भागीदार देशों द्वारा चल रहे बहुराष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में। अमेरिका ने निकासी प्रयास के संचालन के आधार के रूप में काम करने के लिए हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियंत्रण हासिल करने के लिए 6,000 सैनिकों को तैनात किया।
26 अगस्त, 2021 को, काबुल हवाई अड्डे के गेट के बाहर दो आत्मघाती हमले हुए, जिसमें 13 अमेरिकी सैन्य कर्मियों (11 मरीन, एक सैनिक और एक नौसेना कोरमैन) सहित कम से कम 170 लोग मारे गए, और 150 से अधिक घायल हो गए। [52] 27 अगस्त, 2021 को, अमेरिकी सैन्य बलों ने 26 अगस्त, 2021 को हुए काबुल हवाई अड्डे पर हमले के जवाब में आईएसआईएस-के आतंकवादी संगठन के लिए एक अनुमानित "योजनाकार" पर अफ़ग़ानिस्तान के नंगरहार प्रांत में ड्रोन हमला किया।
2021: 22 अक्टूबर, 2021 को, क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में, उत्तर-पश्चिमी सीरिया में एक अमेरिकी हवाई हमले में अल-क़ायदा के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद अल-मतर की मौत हो गई।
ये अमेरिकी दादागीरी के कुछ नमूने ही हैं, जो यहां प्रस्तुत किए जा सके। इसकी काली करतूतों की सूची इतनी लम्बी है कि वह एक अलग किताब का विषय हो सकता है।
टकराव : सत्य और असत्य का या सभ्यताओं का ?
‘सभ्यताओं का टकराव: तथ्य या मिथ्या?’ यह आज की विश्व राजनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसपर सैद्धांतिक बहस और राजनीतिक पटल पर व्यावहारिक संरेखण दोनों के प्रकाश में, हमारा यह कहना सही है कि सभ्यता का टकराव अब एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक वास्तविकता है जो अप्राकृतिक, अनावश्यक, अवांछनीय और विनाशकारी है, लेकिन अब इससे बचना संभव नहीं है। यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि यह दुखद और अप्रिय सच्चाई मौजूद है और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, सभ्यता शब्द से जो अवधारणा हमारे मन में उभरती है, वह उस अर्थ से बिल्कुल अलग है जिसमें पश्चिम के लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे दृष्टिकोण से, यह कहना अधिक उचित है कि संघर्ष सभ्यता और असभ्यता, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, संदेदनशीलता और संवेदनहीनता, सहानुभूति और क्रूरता और न्याय और अन्याय के बीच है। सभ्यताओं के बीच टकराव का कोई अर्थ नहीं है। सभ्यताओं में विविधता, सोच और विचारों में भिन्नता, विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग समय में एक से अधिक सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व एक स्वाभाविक और ऐतिहासिक तथ्य है। साथ ही उनके बीच संबंध, संवाद और समन्यवय, सहयोग और प्रतिस्पर्धा भी स्वाभाविक बात है। कुछ स्थितियों में यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप भी ले सकती है और इतिहास में ऐसा होता भी रहा है, लेकिन सभ्यताओं के मात्र मतभेदों की अवधारणा को अनिवार्य रूप से संघर्ष की ओर ले जाना और इसे एक अपरिहार्य ऐतिहासिक तथ्य बना देना औपनिवेशिक मानसिकता की त्रासदी है। हर सांस्कृतिक अंतर को संघर्ष बनाना और उस अंतर के परिणामस्वरूप संघर्ष को मानवता की नियति बनाना सभ्यता की अवधारणा को ही नकार देने के समान है।
यह समझना आवश्यक है कि सत्य और असत्य के बीच संघर्ष इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है और सत्य का प्रभुत्व प्रकृति की मांग है और मानवता की आवश्यकता है, लेकिन यह अवधारणा सही नहीं है कि सत्य का प्रभुत्व केवल युद्ध और खूनी संघर्ष के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। सत्य मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप है और सत्य को स्वीकार करने का वास्तविक स्थान मनुष्य का हृदय, उसका इरादा और विश्वास है, और विश्वास जबरदस्ती से प्राप्त नहीं किया जाता है, यह हृदय की गहराइयों से स्वीकार करने का दूसरा नाम है। वह तर्क की शक्ति, प्रकृति के साथ सामंजस्य और मानव जीवन को न्याय, संतुलन और सद्भाव के साथ समृद्ध करने की क्षमता के आधार पर अपनी सच्चाई का दावा करता है। यह वही है जो क़ुरआन के इस सिद्धांत में वर्णित है:
दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। सही बात, ग़लत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है। (क़ुरआन, 2:256)
निसंदेह, जब सत्य को मनुष्य तक पहुंचने से रोका जाता है और सत्य तथा मानवता के बीच उत्पीड़न तथा आक्रामकता की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, तब इन बाधाओं को दूर करने के लिए बल का प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है। इस समय, पश्चिमी सभ्यता के झंडावाहक, विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका का शासक वर्ग, सभ्यताओं के टकराव के नाम पर मानवता पर एक निश्चित सभ्यता को थोपने के लिए लड़ रहा है। वह तकनीकी वर्चस्व का लाभ उठा कर अन्य सभ्यताओं के ख़िलाफ़ खूनी खेल खेलते हुए, उन्हें पराजित कर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है या यह कि वे पश्चिम की गुलाम बन कर रहें। यह वास्तविक युद्ध, जिसे पूरी तरह से समझना होगा।
आज की आधुनिक पश्चिमी सभ्यता इस कुत्सित सोच से ग्रस्त है कि “केवल पश्चिम के राष्ट्र ही सभ्य हैं और सभ्यता का ज्ञान रखते हैं और बाकी सभी असभ्य और सभ्यता के दुश्मन हैं।” इस सोच की अभिव्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक नेताओं और बौद्धिक नेताओं के बयानों के माध्यम से दुनिया के सामने आती रहती है। हालाँकि, अगर आप यूरोप की ऐतिहासिक भूमिका और आज पश्चिम के साम्राज्यवादी सांस्कृतिक दिमाग की तुलना में दुनिया के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि मिस्र, सीरिया, चीन, भारत या अफ्रीकी देश, सांस्कृतिक विविधता और मतभेद हर जगह एक वास्तविकता रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतभेदों के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक संघर्ष या टकराव मानवता की नियति बन गया हो। न ही ऐसा हुआ कि एक-दूसरे को अधीन करने और नष्ट करने के लिए बल का प्रयोग किया गया हो। मुस्लिम विचारकों ने सम्पूर्ण विश्व को ‘दारुल दावा’ (जहां इस्लाम की शिक्षा का प्रसार किया जाए) घोषित किया। मुसलमानों ने शांति और युद्ध के नियम और कानून बनाए और सह-अस्तित्व और न्याय के आधार पर लोगों के बीच व्यवहार की नींव रखी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सभ्य दुनिया में असहिष्णुता (intolerance) भी एक विशुद्ध पश्चिमी अवधारणा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता पर अर्नोल्ड जे. टॉयनबी‘Arnold J. Toynbee, विल ड्यूरेंट Will Durant और यहां तक कि बर्ट्रेंड रसेल Bertrand Russell के लेखन इस बात की गवाही देते हैं कि असहिष्णुता यूरोप की विशेषता रही है। आजादी के तमाम दावों के बावजूद वे बुनियादी मुद्दों पर मतभेद को स्वीकार कर उसे प्रामाणिक मानने को तैयार नहीं हैं। फिर राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यही हुआ, जिसकी पहली बड़ी अभिव्यक्ति चौदहवीं सदी से लेकर बीसवीं सदी के आधे हिस्से तक अंध उपनिवेशवाद (साम्राज्यवाद) के रूप में दुनिया के सामने आई।यूरोप के भीतर फासीवाद का विकास और प्रभुत्व इसी मानसिकता का फल था। फिर इसकी हालिया अभिव्यक्ति जो पिछले 20-25 वर्षों से सामने आ रही है और 21वीं सदी में पश्चिमी सभ्यता भी इसी संकल्पना के आधार पर दुनिया को विनाश और रक्तपात का अड्डा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
इतिहास दर्शन की महत्वपूर्ण बहसों में मानव इतिहास में पाई गई सभ्यताओं के कई अध्ययन सामने आए हैं। इनमें से अर्नोल्ड टॉयनबी ने 26 सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है और प्रोफेसर सोरोकिन ने 36 सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनके अवलोकन के अनुसार, सभ्यता की मूल अवधारणा सर्वजगत के निर्माता के साथ किसी प्रकार के संबंध के आधार पर बनी थी। चाहे वह एकेश्वरवाद के आधार पर हो या बहुदेववाद के आधार पर, तथापि, सार्वभौमिकता, आध्यात्मिक शक्ति के साथ संबंध और संपर्क, सर्वजगत की आध्यात्मिक वास्तविकता की पहचान किसी न किसी रूप में हर सभ्यता में मौजूद थी। इसके अलावा, निर्माता के साथ संबंध और इस जगत के एक नैतिक अस्तित्व और इस दुनिया के लिए स्थानीय नहीं बल्कि लौकिक और फिर उसके बाद के जीवन की अवधारणा किसी न किसी रूप में हर सभ्यता में मौजूद रही है। मानव इतिहास और सभ्यता में विकृति अवश्य आई है, परंतु इसे मार-काट का आधार नहीं बनाया गया है। यह केवल आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है, जिसने सृष्टिकर्ता से यह संबंध को तोड़ दिया है। आकाशीय परम्परा एवं धर्म के मार्गदर्शन को अप्रभावी एवं अनावश्यक घोषित कर दिया गया है। इसके स्थान पर, विभिन्न तर्कसंगत अवधारणाओं और हितों को जोड़-तोड़ करके एक विचार प्रणाली में ढाला दिया है, जिसमें तीन अवधारणाएँ केंद्रीय हैं, अर्थात्: तर्कवाद (rationalism), व्यक्तिवाद (individualism) और मानवतावाद (humanism)। इनकी ही अभिव्यक्तियाँ राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साम्यवाद के रूप में अस्तित्व में आईं हैं।
यह वह सभ्यता है जिसने सांसारिकता, भौतिकवाद और मानव बुद्धि और अनुभव को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में केंद्रीयता दी। फिर उन्होंने अन्याय यह किया उसे सभ्यता का नाम दिया, यानी कि बाकी सभी लोग असभ्य थे और हैं। साम्राज्यवाद के इस पूरे इतिहास में, चाहे वह फ्रांसीसी हो या ब्रिटिश, जर्मन साम्राज्यवाद, डच साम्राज्यवाद, या स्पेनिश साम्राज्यवाद, या उसका नवीनतम रूप, अमेरिकी उपनिवेशवाद, इसमें दो प्रमुख अवधारणाएँ दिखाई देती हैं। एक है सभ्यता सिखाने का मिशन (civilizing mission) और दूसरा है श्वेत व्यक्ति का बोझ (white man's burden)। मानो धरती पर एकमात्र सभ्यता यही है, शेष विश्व अज्ञानता और अंधकार में है। इस सभ्यता का प्रभुत्व और इसी के नक्शेकदम पर सभी का चलना सभ्यता की निशानी है, और इसे बढ़ावा देने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों और सैन्य बल का उपयोग अपरिहार्य है, बल्कि वर्चस्व का वास्तविक स्रोत है। गत साढ़े तीन-चार सौ वर्षों से मानवता अन्याय और अत्याचार का जो दर्द देख रही है, वह इसी मानसिकता की देन है।
20वीं सदी में साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन हो गया। हालाँकि उनका मानना था कि हमारी शक्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन उनकी सैन्य ताकत के बावजूद, दो विश्व युद्धों और आंतरिक कलह, असमानता, अन्याय, क्रूरता और संस्थागत अराजकता के कारण उनका पतन शुरू हो गया। 1945 से 1980 के बीच लगभग 150 स्वतंत्र देश विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर उभरे। जिसमें मुस्लिम देशों की संख्या 57 है। यह संख्या संयुक्तराष्ट्र के कुल 192 सदस्यों की संख्या की एक तिहाई से थोड़ी ही कम है।
ब्रिटेन ने एक समय दुनिया के एक चौथाई हिस्से पर राज किया था, लेकिन इसके बावजूद वह न केवल खुद को ग्रेट ब्रिटेन कहता था, बल्कि यह भी दावा करता था कि दुनिया के सभी समुद्र उसकी सत्ता के अधीन हैं। आज अगर आप इसके भूगोल पर नज़र डालें तो वह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसमें कुछ द्वीप शामिल हैं। जो सूरज वहां कभी नहीं डूबता था, वह तो डूब गया, इतना ही नहीं, अब वहां हफ्तों तक सूरज उगता ही नहीं है। ब्रिटेन अब सिमट कर एक छोटा सा देश बन गया है। लेकिन अहंकार अभी भी उसका आदर्श है।
इसके बाद दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप अंततः 1989 में रूस का पतन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। यही वह बिंदु है जहां से उपनिवेशवाद का नया युग शुरू होता है। यही वह अवधि है जिस पर ध्यान दिलाने का इरादा है। इस काल को सभ्यताओं के संघर्ष का काल कहा जाता है। जिन लोगों ने इसमें बहुत काम किया है, उनमें से तीन-चार महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का उल्लेख ज़रूरी है।
अफ़ग़ानिस्तान में अभी जिहाद चल ही रहा था और रूस का अभी पतन नहीं हुआ था कि 1985 में मशहूर अमेरिकी पत्रिका ‘फॉरेन अफेयर्स’ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड डिक्सन ने एक लेख में कहा कि अमेरिका और रूस अफ़ग़ानिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि अमेरिका और रूस का हित एक-दूसरे से लड़ने में नहीं है। असली ख़तरा कुछ और है जिसे समझना ज़रूरी है और वह है इस्लामी कट्टरवाद (Islamic Fundamentalism) का ख़तरा।
उस समय तक केवल तीन या चार चीजें ही हुई थीं, जिनमें से एक थी 57 मुस्लिम देशों की आज़ादी, लेकिन वहां भी शासन उन ताकतों के हाथ में था जो किसी न किसी रूप में अमेरिका और रूस के अधीन थीं। मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका, यूरोप और बहुराष्ट्रीय संगठनों का नियंत्रण था। दूसरा, 1969 में अल-अक्सा मस्जिद को जलाने के परिणामस्वरूप, मुसलमानों ने इस्लामिक देशों के संगठन (ओआईसी) की स्थापना की, जो हालांकि कमज़ोर था, लेकिन उसमें इस्लामी एकता का प्रतीक बनने की क्षमता है। इसी तरह 1973 में पहली बार मुसलमानों ने अपनी तेल की ताकत को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर फरवरी 1979 में इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी क्रांति ने 'इस्लामी ख़तरे' को एक वैश्विक चिंता बना दिया।
दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिम की औपनिवेशिक शक्तियों की रणनीति यह थी कि आजादी के बावजूद मुस्लिम और अरब देशों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के साथ-साथ ईरान के शाह और इसराईल जैसे तत्वों के माध्यम से नियंत्रण में रखें। ईरान में क्रांति और अफ़ग़ानिस्तान में जिहादी सेना की सफलता ने नक्शा बदल दिया। अक्टूबर 1973 में रमज़ान की लड़ाई से पता चला कि मुसलमानों और अरबों की तमाम कमज़ोरियों के बावजूद, इसराईल को चुनौती दी जा सकती है। उस समय, अगर अमेरिका ने इसराईल को बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता प्रदान नहीं की होती, तो इसराईल ने यह कह दिया था कि हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे। यही वह पृष्ठभूमि है जिसके आधार पर पश्चिम के ये विचारक और रणनीतिकार, जो एक नए दुश्मन की तलाश में थे, कि जिसका हव्वा दिखाकर और अपने नागरिकों को आतंकित करके अपने नापाक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। वह शत्रु उन्हें इस्लाम और मुस्लिम जगत के रूप में दिखाई दिया। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राजनीतिक बुद्धिजीवी निक्सन ने 1985 में रूस को उसके नियंत्रण में मुस्लिम आबादी के बारे में चेतावनी दी थी कि संपूर्ण मध्य एशिया, अफ़ग़ानिस्तान और मुस्लिम दुनिया तुम्हारे लिए ख़तरा है, अमेरिका के लिए नहीं, इसलिए आओ! आओ हम और तुम मिलकर कोई रास्ता निकालें।
हालाँकि, कोई संयुक्त रास्ता तो नहीं निकला। लेकिन जब 1988 में रूसी शासक मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी मानसिक और राजनीतिक हार स्वीकार कर ली और यह कहा कि दो साल के भीतर हम अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाएँ वापस ले लेंगे, यही वह समय है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अपनी मूल रणनीति को लागू करना शुरू कर दिया। वह रणनीति क्या थी? कि इस्लाम और मुसलमान हमारे असली दुश्मन हैं। सबसे पहले, नाटो के महासचिव ने कहा कि लाल ख़तरा टल गया है, लेकिन हरा ख़तरा पैदा हो गया है। उसके बाद, बर्नार्ड लुईस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहूदी विचारक, जो लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और फिर 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, विदेश विभाग के सलाहकार और संपूर्ण इसराईली लॉबी के दिमाग के रूप में काम करते थे, 1990 में जब रूसी सैनिक अफगानिस्तान से लौट आए तो उन्होंने मुख्य अमेरिकी पत्रिका अटलांटिक मंथली (Atlantic Monthly) में अपने एक लेख में पहली बार "सभ्यताओं का संघर्ष" (clash of civilizations) की शब्दावली का प्रयोग किया। वे उस लेख में कहते हैं:
अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम मुद्दों, नीतियों और उनका नेतृत्व करने वाली सरकारों के स्तर में विकास की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह सभ्यताओं के टकराव से कम नहीं है। संभवतः यह हमारे यहूदी-ईसाई अतीत, हमारे धर्मनिरपेक्ष वर्तमान और दोनों के वैश्विक विस्तार के ख़िलाफ़ एक प्राचीन दुश्मन की एक अतार्किक लेकिन निश्चित ऐतिहासिक प्रतिक्रिया है। (जेफरसन लेक्चर 1990, बर्नार्ड लेविस “द रेग ऑफ इस्लाम” (The Rage of Islam), अटलांटिक मंथली, सितंबर 1990)
उसी लेख में, जो पहले जेफरसन लेक्चर के रूप में दिया गया और फिर अटलांटिक में और बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, बर्नार्ड लेविस स्पष्ट रूप से कहते हैं:
स्पेन में मुसलमानों के पहले आगमन से लेकर वियना में दूसरी तुर्की घेराबंदी तक, यूरोप एक हज़ार वर्षों तक लगातार इस्लामी ख़तरे के अधीन रहा है।
जिन दो प्रतिस्पर्धी ताकतों का उल्लेख किया जा रहा है, वे एक ओर तथाकथित इस्लामी कट्टरवाद (Islamic Fundamentalism) और दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष पूंजीवादी लोकतंत्र हैं। बाद वाले को आधुनिकता के वाहक और यहूदी-ईसाई सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
यह वास्तव में वह पहला पत्थर था, जो फेंका गया था। फिर इस बात को सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन ने आगे बढ़ाया था। यह एक और यहूदी हैं जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1993 में प्रसिद्ध पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा: द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स। इस पर बहस छिड़ गई, दर्जनों लेख लिखे गए और किताबों की भी एक बाढ़ सी आ गई। इस पूरी बहस को हंटिंगटन ने 1996 में अपनी पुस्तक “क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स ऐंड रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर” में पूरे विस्तार से प्रस्तुत कर दिया है। तब से, यह पुस्तक सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत की विद्वतापूर्ण बाइबिल बन गई है। उसके बाद इस विषय पर बीसियों नहीं बल्कि सैकड़ों बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों (थिंक टैंक) की किताबें, भाषण, रणनीतिक पत्र और रिपोर्टें आ चुकी हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मुस्लिम शासकों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अंदाज़ा नहीं है कि इन 25 वर्षों में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना काम किया गया है और अकादमिक बहस, मीडिया और राजनीतिक चालों के माध्यम से मानसिकताओं को वैश्विक संघर्ष के लिए कैसे तैयार किया गया है। यह है वो पृष्ठभूमि है जिसमें 9/11 रचा गया और उसके बाद जो खेल खेला जा रहा है वह कोई संयोग नहीं बल्कि पूरी योजना का हिस्सा है।
इस समय युद्ध का जो मानचित्र है उसमें, एक ओर मुस्लिम दुनिया है, जो मानसिक रूप से बिखराव का शिकार है, राजनीतिक रूप से विभाजित है, आर्थिक रूप से अपने संसाधनों की रक्षा करने में असमर्थ है और सैन्य रूप से बहुत कमज़ोर है। दूसरी ओर, चूंकि इस्लाम एक सभ्यतागत सिद्धांत, एक आंदोलन और एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसमें वैश्विक सभ्यता का आधार बनने की शक्ति है, इसलिए इसे एक ख़तरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि, उनके शब्दों में, (To nip the evil in the bud) इसे वास्तविक ख़तरा बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए।
हंटिंगटन का विश्लेषण और तर्क
सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन के विश्लेषण और तर्कों पर एक नज़र डालना उचित होगा। उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को हव्वा बनाकर पेश करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने इतिहास से उदाहरण भी लिए हैं और हालिया रुझानों को भी चर्चा में लाया है। इसके लिए सर्वेक्षण तकनीक को हथियार बनाकर 35,000 लोगों की राय को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दो चीजें हैं जो आज अमेरिकियों की नज़र में सबसे बड़ा ख़तरा हैं: एक है परमाणु हथियारों का प्रसार, और दूसरा है आतंकवाद। यह सर्वे 9/11 से सात साल पहले 1994 का है। फिर उन्होंने बताया है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? इसराईल ने 1970 में परमाणु बम बना लिया था और भारत ने भी 1974 में परमाणु परीक्षण किया था लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक परमाणु परीक्षण नहीं किया है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के फैलाव का असली ख़तरा इस्लाम और इस्लामी आंदोलनों से है। उनका कहना है कि इन दोनों के स्रोत मुसलमान हैं। उनके शब्द हैं: 60% अमेरिकी लोग इस्लामी पुनरुत्थान को मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए ख़तरा मानते हैं। (60 % of American people regard Islamic revival a threat to US interests in the Middle East)।
वह आगे कहते हैं कि मुसलमान आज तो कमज़ोर हैं लेकिन अगर उन्हें आर्थिक आधार पर नियंत्रण में नहीं लिया गया तो वे अपने संसाधनों को अपने कब्ज़े में ले लेंगे और एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। फिर जनसंख्या के आधार पर उनकी वैश्विक स्थिति बदल रही है। वे आगे कहते हैं कि 1990 में दुनिया में ईसाई आबादी 25 फीसदी और मुस्लिम 20-21 फीसदी थी, लेकिन अब ईसाई आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उनके अनुमान के मुताबिक, 2025 तक मुसलमानों की आबादी दुनिया की आबादी का 30 फीसदी तक पहुंच जाएगी और ईसाइयों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बीच, अगर मुसलमान अपनी सेना और अपनी परमाणु शक्ति विकसित कर लेते हैं, तो वे पश्चिम की सर्वोच्चता को चुनौती दे देंगे। यह है पश्चिमी सभ्यता के लिए वास्तविक ख़तरा।
उनके विश्लेषण का एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं:
“पश्चिम के लिए वास्तविक समस्या इस्लामी Fundamentalism नहीं है, बल्कि इस्लाम है, जो एक अलग सभ्यता है, और जिसके अनुयायी अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं और सत्ता में अपनी कम बागीदारी को लेकर चिंतित हैं। (The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, ‘Simon Schuster’ 1996)
दूसरे शब्दों में, उनका दावा है कि मुसलमानों की अपनी पहचान है और वे मानते हैं कि उनकी सभ्यता "उनके मूल्य सर्वश्रेष्ठ हैं" लेकिन साथ ही वह "अपनी शक्ति की हीनता से परेशान" (upset with the inferiority of their power) शब्दों का भी उपयोग करते हैं, तो यह उनकी मजबूरी है जिसके कारण उनका गुस्सा मुक़ाबले की ताकत बनाने का प्रेरक साबित होगा, जो आतंकवाद का रूप ले सकता है और जो बढ़ते-बढ़ते व्यापक संघर्ष का रूप ले सकता है। हंटिंगटन ने उसी पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है: Terrorism is the weapon of the weak against the strong (आतंकवाद ताकतवरों के ख़िलाफ़ कमजोरों का हथियार है)। इस तरह इस्लाम और आतंकवाद को जोड़ने का शातिराना खेल खेला गया है। वह आगे कहते हैं:
इस्लाम के लिए समस्या सीआईए या अमेरिकी रक्षा विभाग नहीं है, बल्कि पश्चिम ही है, जो एक अलग सभ्यता है, जिसके अनुयायी अपनी संस्कृति की सार्वभौमिकता में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उनकी श्रेष्ठ शक्ति, चाहे वह कितनी ही पतित क्यों न हो, उन्हें पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति के सांचे में ढालने के लिए बाध्य करती है। ये मुख्य तत्व हैं जो इस्लाम और पश्चिम के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं।
उनके विचार में केंद्रीय मुद्दा संस्कृति और शक्ति है। उनका कहना है कि संस्कृति तब तक अपनी उचित भूमिका नहीं निभा सकती जब तक वह शक्ति प्राप्त न कर ले:
विश्व में संस्कृतियों का विभाजन शक्ति के विभाजन को दर्शाता है। व्यापार शक्ति के अधीन हो भी सकता है और नहीं भी। इतिहास में, किसी सभ्यता की शक्ति का विस्तार उसकी संस्कृति के विकास के साथ-साथ चलता है, और इस शक्ति का उपयोग हमेशा उसके मूल्यों, परंपराओं और संस्थानों को अन्य समाजों तक पहुँचाने के लिए किया गया है। एक सार्वभौमिक सभ्यता के लिए सार्वभौमिक शक्ति की अपेक्षा करती है।
इस्लाम और पश्चिम दो अलग सभ्यताएँ हैं। केवल इस्लाम और पश्चिम ही नहीं, अन्य सभ्यताएँ भी हैं, लेकिन उनके बीच मतभेद का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच संघर्ष आवश्यक हो। उन सभ्यताओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सह-अस्तित्व भी हो सकता है। असहमति का अनिवार्य परिणाम संघर्ष नहीं है। मानव इतिहास में सभ्यताओं के विकास का मार्ग सभ्यताओं के बीच समझौते, संवाद, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मार्ग है। केवल अपनी अवधारणाओं, मूल्यों और तरीकों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना और उसे सांस्कृतिक टकराव कहना विनाश का रास्ता है। निस्संदेह, युद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए और इतिहास का हिस्सा बन गये। केवल सभ्यताओं की विविधता, मूल्यों में अंतर और सिद्धांतों और सामाजिक प्रणालियों में अंतर का मतलब यह नहीं है कि सभ्यताएँ एक-दूसरे से टकराएं हैं। यह पश्चिम की उपनिवेशवादी अवधारणा है।
यानी किसी संस्कृति, उसकी अवधारणाओं, उसके मूल्यों, उसके सिद्धांतों, उसकी संस्थाओं और उसकी प्रणालियों को बलपूर्वक दूसरों पर थोपना, यह साम्राज्यवाद है, सभ्यताओं का टकराव नहीं और अगर ऐसा टकराव होता है तो वह साम्राज्यवाद के कारण ही होता है।
इस्लाम की उपलब्धि यह है कि इसने मनुष्य को असहमत होने का अधिकार दिया है। हर किसी को यह अधिकार है कि वह तर्क के आधार पर बात करे। चर्चा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आवाह्न इसी चीज़ का नाम है। लेकिन किसी को भी अपने विश्वासों और विचारों को बलपूर्वक दूसरों पर थोपने का अधिकार नहीं है। सभ्यताओं के लिए अगर कोई रास्ता है तो वह संवाद, प्रतिस्पर्धा और सहयोग है। संघर्ष, एक-दूसरे को खत्म करने का रास्ता, सभ्यता का नहीं, बल्कि क्रूरता और उपनिवेशवाद का रास्ता है। जिसे आज सभ्यताओं का संघर्ष कहा जा रहा है उसका मुख्य कारण यही औपनिवेशिक मानसिकता है। इसके मूल में यह विश्वास है कि हम दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में अपनी सभ्यता, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्थाएं स्थापित करें। यही समस्या की जड़ है।
सांस्कृतिक प्रभुत्व के लिए जिस रणनीति पर इस समय अमल हो रहो है, उस रणनीति को चुनौती देने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। एक अमेरिकी महिला विचारक, डॉ. शिरीन हैनिंगर, जो वाशिंगटन के एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं, ने कहा है:
यहां तक कि मुस्लिम समाज का पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो जाना और पश्चिमी सभ्यता के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपना लेना भी पश्चिमी और मुस्लिम देशों के बीच स्थायी मेल-मिलाप की गारंटी नहीं दे सकता, जब तक पश्चिमी और मुस्लिम देशों के बीच आपसी टकराव के कारण बने रहेंगे। विशेष रूप से, पश्चिम की तुलना में शक्ति के असंतुलन को दूर करने की मुस्लिम देशों की इच्छा।
हम उनके विश्लेषण से सहमत हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स का शीर्षक भ्रामक है। असली मुद्दा शक्ति संतुलन और मुस्लिम दुनिया पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व और वर्चस्व का है। निस्संदेह, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना इस रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन मुख्य लक्ष्य दुनिया पर हावी होना और इसे अपने नियंत्रण में लाना है, और इस्लाम, मुस्लिम उम्मत और उनकी जिहाद की अवधारणा को इसमें मुख्य बाधा माना जाता है।
हंटनिंगटन द्वारा प्रस्तावित रणनीति में पहली बात अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व है। उनका कहना है: हमारा मुख्य लक्ष्य राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य नियंत्रण हासिल करना है। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अन्य चुनौतीपूर्ण शक्ति उभर कर सामने न आये। यह दृष्टिकोण ब्रेज़िंस्की की पुस्तक द चेसबोर्ड ऑफ नेशंस में प्रस्तुत किया गया है, जो कई साल पहले आई थी। ब्रेज़िंस्की राष्ट्रपति कार्टर के अधीन एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि इस समय अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है। यह आवश्यक नहीं कि भविष्य में यही एकमात्र महाशक्ति बनी रहे। इसलिए अमेरिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम अगले 25 वर्षों तक उसे कोई चुनौती न दे सके और विशेष रूप से यूरोप, चीन और मुस्लिम दुनिया को ध्यान में रखना चाहिए।
दूसरी चीज़ है दुनिया के अन्य देशों में हस्तक्षेप की रणनीति (हस्तक्षेप का अधिकार)। तदनुसार, जहां भी आपको कोई ख़तरा दिखाई पड़े या ख़तरे की गंध महसूस हो, हस्तक्षेप करें और उसे अपने लिए ख़तरा बनने से पहले ही नष्ट कर दें। बुश प्रशासन यही नीति अपना रहा है। और अब उन्होंने अपने रणनीतिक सिद्धांत में खुले तौर पर कहा है कि संयुक्तराष्ट्र की मदद के साथ या उसके बिना "रोकना या हस्तक्षेप करना" उनका अधिकार है। वह इस ख़तरे को 'असहिष्णुता' और 'अतिवाद' कहते हैं। और अगर मुस्लिम जगत के कुछ शासक अपने देशवासियों को धमकाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वास्तव में वे अपने अवलोकन या अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हंनिंगटन के विचारों का अनुसरण कर रहे हैं।
तीसरी बात, जिसे वह शोषण की रणनीति कहते हैं, आर्थिक संसाधनों पर कब्ज़ा करना है। क्योंकि तेल, ऊर्जा, खनिज संसाधन और संचार के साधन और मार्ग रणनीतिक संपत्ति हैं और हमें उन पर कब्ज़ा करना होगा।
चौथी चीज़ है मीडिया की ताकत का इस्तेमाल। सभी प्रकार के मीडिया इसका हिस्सा हैं। यह विचारों और दिमागों को नियंत्रित करने, उन्हें आकार देने या एक विशिष्ट सांस्कृतिक सांचे में ढालने की प्रक्रिया है।
पांचवीं बात, उनका कहना है कि अमेरिका लंबे समय तक अकेले यह काम नहीं कर पाएगा, इसलिए अमेरिका को यूरोप के साथ एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए। जिसमें अब इसराईल और रूस के साथ भारत भी जुड़ गया है। उनके अनुसार, प्रतियोगिता में मुख्य ताकत मुस्लिम दुनिया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। उनके शब्दों में: इस्लामी और चीनी देशों की पारंपरिक और अपरंपरागत सैन्य शक्ति को बढ़ने से रोकना।
आखिरी बात वे यह कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम आप्रवासी खुद हमारे लिए ख़तरा बन गए हैं। वह कहते हैं:
पश्चिमी संस्कृति को पश्चिमी समाजों के के भीतर मौजूद समूहों से चुनौती मिल रही है। एक चुनौती अब आप्रवासियों से आती है जो [हमारे समाज में] आत्मसात होने से इनकार करते हैं और अपने देशों की संस्कृति, रीति-रिवाजों और मूल्यों का प्रसार करना जारी रखते हैं। यह मौजूदगी यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा है।
इन पाँच बिन्दुओं के आलोक में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी देशों द्वारा तैयार किये गये युद्ध के मानचित्र की मुख्य विशेषताओं को देखा जा सकता है।
इतिहास गवाह है कि सांस्कृतिक विविधता का परिणाम सभ्यताओं का टकराव नहीं है, यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। लेकिन जब कोई आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वर्चस्व रखने वाली सभ्यतागत ताकत पूरी दुनिया पर अपनी व्यवस्था जबरदस्ती थोपना चाहती है, दूसरों को अपने रंग में रंगना चाहती है और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति और उनके समाज को अपनी जंजीरों में बांधना चाहती है, तो संघर्ष पैदा होता है। इस समय पश्चिम ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का माहौल बनाने के लिए यही तरीका और रास्ता अपनाया है।
मुस्लिम उम्मत एक संदेश और दावत का झंडावाहक है। हमारा सांस्कृतिक संघर्ष केवल सत्ता, केवल संसाधन, केवल भौतिक लाभ और धन के लिए नहीं है। हमारी सभ्यता के मूल सिद्धांत उच्च नैतिक मूल्य हैं। मानव समाज का निर्माण न्याय और परोपकार के आधार पर करना है, ताकि इस दुनिया में सम्मान और शांति प्राप्त हो और उसके बाद आख़िरत वास्तविक सफलता प्राप्त हो।
इस्लामी सभ्यता की पहचान के तीन पहलू हैं: पहली चीज़ है तौहीद, जिसका अर्थ है अल्लाह से जुड़ना। इसका अर्थ है अपने आप को आत्मनिर्भर और दुनिया से पूरी तरह से स्वतंत्र न मानना, इस दुनिया को सब कुछ न मानना और अल्लाह को केवल निर्माता ही नहीं मानना, बल्कि उसे, सदा जीवित रहने वाला और समस्त जीवनों का स्रोत, आदेश देने वाला, स्वामी, मार्गदर्शन का स्रोत और शक्ति के उद्भव स्वीकार करना है। तौहीद का मतलब पूरी इंसानियत को अल्लाह की इबादत के रास्ते पर लाने की कोशिश करना है। यह हमारा पहला आधार है।
दूसरा आधार यह है कि इस्लाम केवल एक आस्था नहीं है, बल्कि यह एक सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है। यह उसी मान्यता पर आधारित एक सामूहिक जीवन है, जो सभी मानवीय रिश्तों और मानवीय संस्थाओं, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रकट होता है, जो एक सुसंगत और संपूर्ण व्यवस्था के रूप में विश्वास के बीज से एक वृक्ष के रूप में विकसित होता है। इसे हम एक शब्द में शरीयत कह सकते हैं, जिसका अर्थ है अल्लाह द्वारा दिया गया कानून। जीवन की व्यवस्था को अल्लाह के आज्ञापालन के सिद्धांत पर स्थापित करना ही सफलता की गारंटी है।
तीसरा आधार उम्मात की अवधारणा है, जो रंग, नस्ल, भौगोलिक क्षेत्र, हित और इतिहास से परे है। यूरोप और अमेरिका के वे लोग जिनका इतिहास, संस्कृति और परंपराएं हमसे अलग हैं, वे ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते ही हमारा हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी जाति और रंग से संबंध रखने वाला, इस शब्द को पढ़ कर मुस्लिम उम्मत का हिस्सा बन सकता है।
ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं और इनके लिए आवश्यक है कि एक ओर हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को इन सिद्धांतों पर स्थापित करें, सभी संसाधनों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए करें और उन्हें विकसित करें। सामूहिक शक्ति प्राप्त करना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही दुनिया के सामने सही उदाहरण पेश करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है।' हालाँकि, हम धर्म और इस्लामी सभ्यता को बल से नहीं बल्कि तर्क से बढ़ावा देने के लिए बाध्य हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संदेश को प्रसारित करें और तर्क के साथ करें। दूसरी ओर, यह भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सत्य और अपनी व्यवस्था की रक्षा करें साथ ही अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। जिहाद में वास्तव में यही दो पहलू शामिल हैं। एक ओर अल्लाह की इबादत के तरीक़े को स्वीकार करना है और दूसरी ओर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना। यही कारण है कि जिहाद हमेशा दुश्मन की आंखों में चुभता रहा है। और यही कारण है कि इस्लाम की विरोधी ताकतें, जिनकी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं मुसलमानों की जिहाद की भावना से बाधित होती हैं, ने हमेशा जिहाद की अवधारणा को निशाना बनाया है। पिछले 400 वर्षों का इतिहास विस्तार से पढ़ें। जहां भी पश्चिमी उपनिवेशवाद से लड़ाई हुई है, वह मुसलमानों द्वारा ही की गई है और जिहाद के आधार पर ही की गई है। पश्चिम के विचारक, चाहे वे प्राच्यवादी (Orientalist) हों, मिशनरी हों या शासक हों, सभी ने जिहाद को लक्ष्य बनाया है।
इस सांस्कृतिक आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता अल्लाह के साथ अपने संपर्क को जोड़ने और मज़बूत करने की है। जिस तरह एकेश्वरवाद इस्लामी सभ्यता की बुनियाद है, उसी तरह इस्लाम की रक्षा रणनीति का पहला सिद्धांत अल्लाह से संपर्क बनाए रखना, अल्लाह से रिश्ता गहरा करना, अल्लाह से मदद मांगना और ये सारे काम अल्लाह के भरोसे करना है।
दूसरी चीज़ है मुसलमानों की एकता और उनकी सामूहिकता। अगर मुसलमान एकजुट नहीं होंगे, और वे संप्रदायों और समूहों में विभाजित हो जाएंगे, एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो उनकी ताकत बिखर जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सामूहिकता एवं एकता हमारी रणनीति का दूसरा मुख्य बिंदु है।
तीसरी चीज़ है आमंत्रण (इस्लाम की ओर बुलाना) हम ठहरे हुए नहीं रह सकते। हम एक आह्वान के झंडावाहक हैं और हमारी ताकत अल्लाह के समर्थन के बाद इनसानों की ताकत से है। अतः शिक्षा, उपदेश, आमंत्रण और लोगों को अपने में समाहित करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, यह हमारा स्थायी कार्यक्रम है।
नैतिक बल ही इस मार्ग का मुख्य सहयोगी है। इसी से मानव हृदय जीता जा सकता है। इन मानव संसाधनों के साथ-साथ भौतिक शक्ति भी आवश्यक है। अगर हम भौतिक शक्ति की उपेक्षा करेंगे तो हम उस कानून से भटक जायेंगे जो अल्लाह ने इस संसार के लिए बनाया है। कुदरत ने जो कानून बनाए हैं उनके जरिए संसाधन हासिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसका अर्थ है उन संसाधनों की खोज करना जो अल्लाह ने सर्वजगत में जमा कर दिए हैं, उन्हें विकसित करना और उन्हें सही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करना। इसलिए क़ुरआन ने सूरह अनफाल में साफ कहा है कि अपने घोड़े तैयार रखो। तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए और ताकत ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन को उससे डर लगे। यह ताक़त आस्था और नैतिकता से आती है, और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति से आती है। इसलिए विश्वास और कर्म के साथ-साथ विकास भी बहुत जरूरी है। अगर इसे नज़रअंदाज़ किया जाएगा तो इस सांस्कृतिक आक्रमण का मुक़ाबला नहीं किया जा सकेगा।
आज के युग में शक्ति असंतुलन का अर्थ बदल गया है। इतनी शक्ति तो होनी ही चाहिए, जो प्रतिद्वंद्वी की ताकत को बेअसर करने और उसे आक्रामकता से रोकने के लिए पर्याप्त हो। आज समानता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा करने की, और दुश्मन पर प्रहार करने की ताक़त होनी चाहिए। पवित्र क़ुरआन में वर्णित मुक़ाबले की शक्ति का अर्थ यह है कि तुम्हारे दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों को उससे भयभीत हों। यह अनिवार्यतः हमारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। यह प्राप्त होने योग्य है, इसके लिए समानता आवश्यक नहीं है। इसके लिए बस सही रणनीति की जरूरत है।
सभ्यताओं के बीच संवाद, सहयोग, यहां तक कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, सभी सही हैं, लेकिन सभ्यताओं के बीच संघर्ष, युद्ध और रक्तपात, और एक-दूसरे को वश में करने और अधीन करने के लिए बल का प्रयोग मानवता के सम्मान और विकास का मार्ग नहीं है। यही कारण है कि सभ्यताओं का टकराव हमारी रणनीति नहीं है, इसे मुसलमानों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। यह विनाश का संदेश है, लेकिन अगर कोई महाशक्ति अहंकार में अंधी हो गई है और बलपूर्वक दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, तो उसके सामने आत्मसमर्पण करने और आत्मरक्षा का प्रयास छोड़ने से बड़ा कोई अपराध नहीं है।
इस स्थिति से केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अच्छे लोग दुखी हैं और इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। दुनिया के कोने-कोने में लाखों लोगों ने इराक़ में युद्ध का विरोध किया है और अमेरिका में भी कर रहे हैं। मुस्लिम जगत की 90 से 98 प्रतिशत आबादी अमेरिका की इन नीतियों और हस्तक्षेपों का विरोध कर रही है। यूरोप में 70 से 80 प्रतिशत और अफ़्रीका में 70 से 90 प्रतिशत लोग विरोध कर रहे हैं। अत: विश्व का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ अमेरिकी मानवीय नीतियों के प्रति घृणा न पाई जाती हो।
मैं सभ्यताओं के टकराव को उस फ्रेम में नहीं ले जाना चाहता जिसमें हमारे दुश्मन इसे हम पर थोपना चाहते हैं। मेरे विचार में यह संघर्ष सभ्यता और अज्ञान, सभ्यता और बर्बरता तथा शांति और युद्ध के पुजारियों के बीच है। हमें नैतिक मूल्यों, कानून का शासन, न्याय, सम्मान और मनुष्य की गरिमा और अल्लाह की भूमि को सभी मनुष्यों के लिए बनाए रखना है। निस्संदेह, इस युद्ध में हमारा सामना उन लोगों से है, जो दुनिया की शांति को, वल्कि पूरी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। हमें उनसे मुकाबला करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। हमें यह लड़ाई अकेले नहीं लड़नी चाहिए। बेशक पहला निशाना हम हैं, लेकिन निशाने पर दूसरे भी हैं। हमें अच्छी विदेश नीति के माध्यम से सहयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए और मिलकर इसका मुक़ाबला करना चाहिए।
***********
(Follow/Subscribe Facebook: HindiIslam,Twitter: HindiIslam1, YouTube: HindiIslamTv, E-Mail: HindiIslamMail@gmail.com)
Recent posts
-

एलजीबीटीक्यू+ मूवमेंट पारिवारिक संरचना और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ख़तरा है -अमीरे जमाअत इस्लामी हिन्द
25 August 2024 -
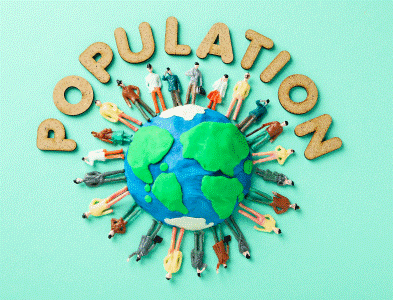
जनसंख्या वृद्धि ग़रीबी नहीं, उत्पादन बढ़ाती है
30 June 2024 -
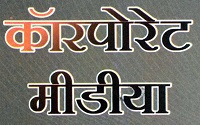
कॉरपोरेट मीडिया
22 March 2024 -
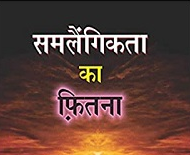
समलैंगिकता का फ़ितना
18 March 2024 -

फ़िलिस्तीनी संघर्ष ने इसराईल के घिनौने चेहरे को बेनक़ाब कर दिया
27 December 2023 -

इसराईली राज्य अपनी आख़िरी सांसें ले रहा है
16 December 2023