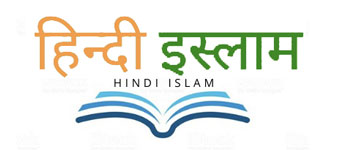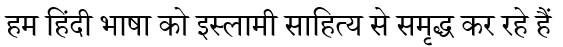तज़किया और एहसान (शरीअत : लेक्चर# 8)
-
शरीअत
- at 12 November 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
‘तज़किया’ (आन्तरिक शुद्धि) और ‘एहसान’ (किसी कार्य को निर्धारित कर्त्तव्य से बढ़कर और सुन्दरता से करना) को हमेशा हर धर्म और हर धार्मिक सन्देश में एक मौलिक आवश्यकता समझा गया और आध्यात्मिक पवित्रता को धार्मिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण, बल्कि सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य क़रार दिया गया। धर्म और आध्यात्मिक सन्देश का मूल उद्देश्य इंसान के नफ़्स (अन्तर्मन), दिल और रूह का ‘तज़किया’ है। इंसान अपने दिल और रूह की गहराइयों से अपने रचयिता की ओर उन्मुख हो, पैदा करनेवाले के आदेशों पर चलने का उत्प्रेरक दिल के अन्दर से पैदा हो, हर समय रचयिता के सामने जवाबदेही का एहसास ताज़ा रहे और आख़िरकार रचयिता से मुलाक़ात और रचयिता के सामने पेशी का एक स्थायी शौक़ और रुचि हो, यह कैफ़ियत पैदा करना हर धर्म का, हर आकाशीय ग्रन्थ का और अल्लाह तआला के हर पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) का मौलिक लक्ष्य और उद्देश्य रहा है। इबादतें इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हैं। तक़्वा (ईशपरायणता) इसी उद्देश्य को प्राप्त करने का एक ज़रिया और मंज़िल है। शरीअत के तमाम आदेश इसी विश्वास और इत्मीनान को क़ायम करने, क़ायम रखने और अधिक पक्का करने के लिए हैं। लेकिन ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के इस महत्त्व के बावजूद कि यह हर धर्म की पहली और आरम्भिक आवश्यकता है अधिकांश धर्मों के माननेवालों में ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के मामले में दो अतिवादी रवैये पैदा हो गए। कुछ प्राचीन धर्मों में संसार त्याग और रहबानियत (संन्यास) की भावना पैदा हुई, कुछ अन्य धर्मों में ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की अत्यन्त सूक्ष्म और गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों को जब किताबी शक्ल में संकलित किया गया तो इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे ऐसे तत्वों की मिलावट हो गई जो ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की कोमलता और पवित्रता के साथ मेल नहीं खाते थे।
मसीही तसव्वुफ़ (सूफ़ीवाद) में, हिंदुओं के यहाँ प्रचलित आध्यात्मिक धारणाओं में दर्शन की इतनी गहरी मिलावट हो गई कि तसव्वुफ़ एक फ़ल्सफ़ा (दर्शन) बनकर रह गया। इससे दुनिया की बहुत-सी क़ौमें प्रभावित हुईं, ख़ुद मुसलमान सूफ़ियों में कुछ लोग जाने-अनजाने इन धारणाओं और विचारों से प्रभावित हुए और यों एक ज़माना ऐसा आया कि आध्यात्मिकता और वुजूदी फ़ल्सफ़ा, आध्यात्मिक पवित्रता और बातिनियत (रहस्यवाद), अल्लाह के सामने जवाबदेही का गहरा दिली एहसास और शरीअत के आदेशों से भागने का रवैया, इन सब बातों ने एक-दूसर के साथ क़रीब-क़रीब एक-दूसरे की पूरक की हैसियत अपना ली।
इस्लाम में आध्यात्मिकता का आरम्भ शुरू ही से हो गया था, शुरू से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का यह प्रशिक्षण किया कि जहाँ वे शरीअत के ज़ाहिरी आदेशों पर अमल करें, जहाँ वे शरीअत के उन आदेशों पर अमल करें जिनका सम्बन्ध इंसान के अंगों और स्नायुओं से है, जिनको बाद में ‘फ़िक़्ह’ का नाम दिया गया, वहाँ वह शरीअत के आन्तरिक आदेशों पर भी अमल करें, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, ‘तज़किया-ए-नफ़्स’ (आत्म-शुद्धि), ‘एहसान’ (कर्त्तव्य से बढ़कर कार्य करना) और दूसरी उच्च एवं श्रेष्ठ आध्यात्मिक कैफ़ियतें उनको प्राप्त हों। जिन बुराइयों से जिन ना-पसन्दीदा दिली अनुभूतियों से शरीअत ने बचने का आदेश दिया है उनसे बचें, जिन अच्छाइयों या हार्दिक अनुभूतियों को शरीअत ने पसन्दीदा क़रार दिया है उनको अपनाएँ।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन के ज़माने तक यह अत्यन्त पवित्र और सुथरा मार्गदर्शन-स्रोत जारी रहा। क़ौमें और नस्लें उनसे लाभान्वित हुईं, दुनिया के देशों तक विभिन्न महाद्वीपों तक उसके लाभ और फल पहुँचे। जब तीसरी-चौथी शताब्दी हिजरी के ज़माने में विभिन्न इस्लामी ज्ञान-विज्ञान के संकलन का काम शुरू हुआ, और इस्लाम की शिक्षा एवं मार्गदर्श के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग संकलित करने का काम आगे बढ़ा, उस समय इस बात की भी ज़रूरत महसूस हुई कि तसव्वुफ़ (सूफ़ीवाद) के आदेशों और ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की शिक्षा को भी संकलित किया जाए। चुनाँचे इस मुबारक काम का आरम्भ मुहद्दिसीन के हाथों हुआ, अनेक मुहद्दिसीन ने ‘ज़ुह्द’ (संयम) और ‘रिक़ाक़’ (कोमल हृदयता) के विषय पर किताबें तैयार कीं, हदीसों के संग्रह संकलित किए। इन प्रयासों का उद्देश्य यह था कि इंसान के दिल में भौतिकता के प्रति प्रेम, और दुनिया से ग़ैर-ज़रूरी दिलचस्पी की भावनाओं को कम किया जाए, आख़िरत की जवाबदेही के एहसास को और अधिक पक्का किया जाए और अल्लाह के सामने पेश होने की याद को हमेशा दिलों में ताज़ा और जगाए रखा जाए। चुनाँचे हज़रत इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰), हज़रत इमाम अबदुल्लाह-बिन-मुबारक (रह॰) और दूसरे अनेक लोगों ने ज़ुह्द और ‘इस्तिग़ना’ (निस्पृहता) के विषय पर किताबें लिखीं।
जैसे-जैसे समय गुज़रता गया ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ से सम्बन्धित इस्लाम के आदेशों को इल्मी अन्दाज़ में संकलित करने के प्रयास भी जारी रहे। दूसरी ओर जैसे-जैसे इस्लामी राज्य फैलता गया, मुसलमानों की राजनैतिक शक्ति में वृद्धि होती गई और इसके परिणामस्वरूप भौतिक सुविधाओं की बहुतायत हुई, तो कुछ नेक लोगों ने यह महसूस किया कि भौतिकवाद के इस बढ़ते हुए वर्चस्व से कहीं मुसलमानों की आध्यात्मिक सत्ता लोगों की नज़रों से ओझल न हो जाएँ, कहीं दौलत की इस अधिकता के नतीजे में जनसाधारण अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न हो जाएँ, कहीं संसाधनों की इस बहुतायत के कारण लोगों का ध्यान अस्ल दीनी सच्चाइयों से हटकर सांसारिक लाभों पर केन्द्रित न हो जाए, इसलिए कुछ लोगों ने विशेष रूप से आख़िरत (परलोक) की याद दिलाने, भौतिकवाद से विरक्ति, और दुनिया से दिल लगाने के कार्य को ना-पसन्दीदा क़रार देने के प्रयासों का आरम्भ किया।
इस तरह धीरे-धीरे करके ऐसे लोग दूसरे विद्वानों और इस्लाम के आवाहकों से अलग होते गए जिनके जीवन का विशेष उद्देश्य यह था कि जनसाधारण के दिलों में अल्लाह के प्रति प्रेम को ताज़ा करें, भौतिकवाद में डूबने से उनको रोकें, संसार की उपयोगी वस्तुओं और धन-दौलत की अधिकता के नैतिक और आध्यात्मिक नकारात्मक परिणामों से उनको अवगत करें। ऐसे लोग अधिकांश दूसरी शताब्दी हिजरी के अन्त और तीसरी शताब्दी हिजरी के आरम्भ में सामने आने शुरू हो जाते हैं। ये वे लोग थे जिनका समाज में असाधारण सम्मान और स्थान था, बड़े-बड़े मुहद्दिसीन, इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰), इमाम यहया-बिन-मुईन जैसे बुज़ुर्ग इन शख़्सियतों की सेवा में हाज़िर होते थे, हज़रत हातिम असम जो इमाम अहमद के प्रसिद्ध साथी और उनके क़रीबी दोस्त थे, वह इसी तरह के एक व्यक्ति थे। हज़रत इबराहीम अदहम इसी तरह के एक व्यक्ति थे, हज़रत बशर अल-हाफ़ी ऐसे ही अल्लाहवाले बुज़ुर्ग थे। कुछ और लोग भी थे, उन्हीं लोगों में एक इब्ने-अबी-दुनिया थे जिनकी बहुत-सी किताबें हैं।
इन लोगों ने यह बेड़ा उठाया कि मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन और फ़ुक़हा के ज्ञानपरक और वैचारिक प्रयासों के साथ-साथ शरीअत के तीसरे पहलू, यानी नैतिकता और ‘तज़किया’ और मुसलमानों के आध्यात्मिक प्रशिक्षण के पहलू पर भी पूरा ध्यान दें और जनसाधारण की मानसिक, बौद्धिक तथा वैचारिक तैयारी के साथ-साथ उनको आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करें। इस तरह आध्यात्मिकता के ज्ञान का एक क्रमबद्ध और विधिवत आरम्भ हुआ, जिसको इस्लाम के मुख्य दौर में ही तसव्वुफ़ का नाम दिया गया, आध्यात्मिकता और नैतिक प्रशिक्षण के इस कार्य से जुड़े लोग जनसाधारण में ‘सूफ़ी’ की उपाधि से प्रसिद्ध हुए, यानी वे ‘ज़ाहिद’ पश्मीना ओढ़नेवाले जो भौतिकवाद से परे रहकर ज़िन्दगी गुज़ार सकते हों, जिनकी ज़िन्दगी का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण को अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रेम और शरीअत से जुड़े रहने की नसीहत करना हो। ये लोग बहुत जल्द समाज में असाधारण सम्मान और अक़ीदत (श्रद्धा) का केन्द्र बन गए, जनसाधारण की बड़ी संख्या ने उनसे सम्पर्क किया।
मानव समाज की विशेषता यह रही है कि जब मानव समाज में किसी चीज़ का चलन होता है तो जहाँ उसके वास्तविक ध्वजावाहक मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के हक़दार क़रार पाते हैं, वहाँ इस मान-सम्मान की ख़ातिर इस गिरोह में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो दरअस्ल इस सन्देश के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते, उनका उद्देश्य मात्र ख्याति प्राप्त करना, या जनसाधारण में सम्मान प्राप्त करना या इस तरह के दूसरे भौतिक या सांसारिक उद्देश्य होते हैं। यह हर मैदान में होता रहा है, मुहद्दिसीन के साथ भी हुआ है, जहाँ बड़े-बड़े मुहद्दिसीन थे, वहाँ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इल्मे-हदीस की बढ़ती हुई लोकप्रियता से फ़ायदा उठाकर अपने को नुमायाँ करना चाहा, क़ुरआन के टीकाकारों में भी ऐसे लोग थे, फ़ुक़हा में भी थे। इसलिए तसव्वुफ़ में अगर ऐसे लोग आकर शामिल हो गए हों तो यह कोई अनहोनी बात नहीं है। तसव्वुफ़ के नाम से बहुत-से लोगों ने कारोबार चलाना चाहा, उनमें विशुद्ध भौतिकवादी और भौतिक लाभों से दिलचपसी रखनेवाले लोग भी थे, भौतिक लाभों से दिलचपसी रखनेवालों के साथ-साथ इस वर्ग में ‘बातिनियत’ और ‘इस्माईलियत’ के ध्वजावाहक भी थे जो इस वर्ग की बढ़ती हुई लोकप्रियता से लाभ उठाकर अपने विचारों और धारणाओं को तसव्वुफ़ के नाम से मुसलमानों में फैलाना चाहते थे, यों तसव्वुफ़ में ग़ैर-इस्लामी चीज़ों की मिलावट शुरू हो गई। अब ज़रूरत इस बात की महसूस होने लगी कि तसव्वुफ़ में जिन ग़ैर-इस्लामी चीज़ों की मिलावट हो गई है उनको अलग किया जाए, तसव्वुफ़ और ‘तज़किया’ की अस्ल रूह को पवित्र क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में स्पष्ट करने की कोशिश की जाए। इस तरह तसव्वुफ़ के बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान सामने आए, जिन्होंने क़ुरआन और सुन्नत की सम्बन्धित शिक्षा को, बड़े-बड़े सूफ़ियों के ख़यालात को और अपने अनुभवों और आँखों देखी घटनाओं को लिखित रूप में संकलित करना शुरू किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुद तो कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके अक़्वाल (कथन) इतने अधिक उद्धृत किए गए हैं कि उनकी रौशनी में तसव्वुफ़ के बारे में उनकी धारणाओं का स्पष्ट रूप से अन्दाज़ा किया जा सकता है। चुनाँचे हज़रत हसन बस्री, जुनैद बग़्दादी, हज़रत हातिम असम, बशर अल-हाफ़ी, इबराहीम अदहम, और उन जैसे बहुत-से लोगों के ख़यालात तसव्वुफ़ की प्राचीन किताबों में बहुत अधिक मिलते हैं और उनके आधार पर एक स्पष्ट धारणा क़ायम की जा सकती है कि इन लोगों की नज़र में तसव्वुफ़ और ‘तज़किया’ से क्या मुराद है।
फिर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, अबू-नस्र सिराज, अबू तालिब मक्की, इमाम अबुल-क़ासिम क़ुशैरी वग़ैरा ने इस विशुद्ध दीनी ज्ञान को विधिवत रूप से संकलित किया। फिर आगे चलकर इमाम ग़ज़ाली, शैख़ अब्दुल-क़ादिर जीलानी, और हमारे उपमहाद्वीप में हज़रत शैख़ अली हजवेरी, मुजद्दिद अल्फ़-सानी शैख़ अहमद सरहिन्दी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और दूसरे बहुत-से लोगों ने तसव्वुफ़ की शिक्षाओं को ज्ञानपरक और लिखित रूप देने की कोशिश की। यही लोग तसव्वुफ़ के बड़े-बड़े प्रतिनिधि हैं। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ क्या नहीं है? यह जानने के लिए इन्हीं लोगों के लेख और किताबें देखनी चाहिएँ।
तसव्वुफ़ के प्रमाणित प्रतिनिधियों ने लिखा है कि सूफ़ियों के तज़किरे, अप्रमाणित कथनों के संग्रह और सूफ़ियों से जुड़ी हिकायात (कथाएँ) तसव्वुफ़ की शिक्षाओं या आदेशों का मूलस्रोत नहीं हैं। तसव्वुफ़ की शिक्षा और आदेशों का मूलस्रोत क़ुरआन और सुन्नत के आदेश और शरीअत के सिद्धान्त हैं, और इसके बाद इन ज़िम्मेदार लोगों के, जिनका सम्बन्ध ताबिईन और तबा-ताबिईन के ज़माने से था, कथन और कही हुई बातें हैं, और सबसे आख़िर में ये ज्ञानपरक किताबें आती हैं जो विद्वानों ने संकलित की हैं। ये सब लोग जिन्होंने तसव्वुफ़ पर प्रमाणित किताबें तैयार कीं। उदाहरणार्थ हमारे उपमहाद्वीप के शैख़ अली हजवेरी, ख़ुरासान के इमाम अबुल-क़ासिम क़ुशैरी, इमाम ग़ज़ाली, और दक्षिण एशिया के निराले विद्वान हज़रत मुजद्दिद अल्फ़-सानी, ये सब लोग ज्ञान की दुनिया में भी ऊँचा स्थान रखते हैं और तसव्वुफ़ की शिक्षाओं को बयान करने में भी उन्होंने इसी आलिमाना स्थान को बरक़रार रखा है। समय गुज़रने के साथ-साथ तसव्वुफ़ के सिलसिले अस्तित्व में आ गए, हर बड़े सूफ़ी की एक निराली प्रशिक्षण विधि थी। यह एक स्वाभाविक-सी बात है कि हर प्रशिक्षण शैली के नतीजे में जब छात्रों की एक जमाअत तैयार होगी, प्रशिक्षित नस्ल सामने आएगी तो उसके नतीजे में एक मकतबे-फ़िक्र (विचारधारा) ख़ुद-ब-ख़ुद अस्तित्व में आएगा। चुनाँचे जिस तरह तफ़सीर (क़ुरआन की टीका) में, हदीस में, फ़िक़्ह में इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) में मकातिबे-फ़िक्र अस्तित्व में आए, उसी तरह तसव्वुफ़ में भी मकातिब (विचारधाराएँ) अस्तित्व में आए जिनको तरीक़ा या सिलसिला कहा गया।
उपमहाद्वीप भारत-पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्की, ईरान वग़ैरा में यह मकातिबे-फ़िक्र ‘सिलसिला’ के नाम से जाने जाते हैं। कुछ और देशों में उदाहरणार्थ अरब दुनिया में और किसी हद तक तुर्की में इनको ‘तरीक़ा’ या ‘तकिया’ का नाम दिया गया है। ये वे मकातिबे-फ़िक्र हैं जिनका सम्बन्ध प्रशिक्षण के तरीक़ों से और प्रशिक्षण के अन्य मामलों से है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के उन मामलों से है जिनमें कुछ सम्मानित प्रशिक्षणकर्ता लोगों ने प्रशिक्षण के नए-नए सिद्धान्त खोज लिए हैं। यह सिलसिला लम्बे समय तक जारी रहा। कुछ सूफ़ियाना सिलसिलों को कुछ इलाक़ों में बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई, उन्होंने वहाँ मुसलमानों का दीनी प्रशिक्षण किया, उसकी दीनी एकता को बरक़रार रखने में मदद की, जनसाधारण के आध्यात्मिक प्रशिक्षण का कर्त्तव्य निभाया और न केवल आध्यात्मिकता के मामले में, न केवल प्रशिक्षण और शिक्षा के मामले में, बल्कि समाज सुधार और सुधारवादी कोशिशों के मामले में भी इन लोगों की कोशिशें बहुत नुमायाँ हैं।
अतीत में तसव्वुफ़ के जितने बड़े-बड़े सिलसिले थे वे सब किसी-न-किसी हैसियत से किसी-न-किसी सतह पर दावत और तबलीग़ के काम में हमेशा शरीक रहे हैं। आधुनिक काल आते-आते उनमें से बहुत-से सिलसिले कमज़ोर पड़ गए, कुछ जगह केवल परम्पराएँ क़ायम रह गईं, अस्ल रूह धीरे-धीरे करके कमज़ोर होती गई, विशेष रूप से पश्चिमी उपनिवेशवाद के आने के बाद जब जिहाद की कोशिशें असफल हुईं तो मुसलमान समष्टीय रूप से एक हद तक निराशा का शिकार हुए और उन्होंने वह सुधारवादी और दीनी कोशिशें छोड़ दीं, जिनका सम्बन्ध पश्चिमी उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त करने से था। इसी ज़माने में तसव्वुफ़ के सिलसिले भी निष्क्रयता का शिकार हुए और वे मात्र एक परम्परा या विरासत के, एक इतिहास के ध्वजावाहक बनकर रह गए। जिनके बारे में अल्लामा इक़बाल ने कई जगह बहुत कड़े शब्दों में नापसन्दीदगी का इज़हार किया है। सच तो यह है कि हम जब प्राचीन सूफ़ियाना केन्द्रों के इन बुज़ुर्गों का जिनके नाम से वे केन्द्र जुड़े हैं, उनके आज के उत्तराधिकारियों से मुक़ाबला करते हैं तो, ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का अन्तर नज़र आता है। अल्लामा इक़बाल ने जगह-जगह इस अन्तर की निशानदेही की है और यह याद दिलाने की कोशिश की है कि सूफ़ियों को अपने पिछले कर्त्तव्य याद रखने चाहिएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं भूलनी चाहिएँ और अपने बुज़ुर्गों की इन वास्तविक परम्पराओं को ज़िन्दा करना चाहिए जिनके वे ध्वजावाहक थे।
तसव्वुफ़ के बारे में यह आरम्भिक चर्चा इस लेक्चर की भूमिका है जिसमें यह बताना अभीष्ट है कि ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के बारे में इस्लाम की शिक्षा क्या रही है, मुसलमानों में आध्यात्मिकता का आरम्भ कैसे हुआ, तसव्वुफ़ को क्रमबद्ध और संकलित कैसे किया गया और तसव्वुफ़ के बड़े-बड़े प्रतिनिधियों के विचार, धारणाएँ और विचारधाराएँ क्या हैं? चर्चा के आख़िर में आधुनिक काल में तसव्वुफ़ के पुनरुत्थान के कुछ प्रयासों के बारे में एक-दो संक्षिप्त संकेत भी किए जाएँगे।
शरीअत की शिक्षा का यह वह मौलिक पहलू है जिसको प्रचलित भाषा में ‘क़ल्बी इस्लाह’ या आन्तरिक सुधार के शीर्षक से याद किया जाता है। शरीअत की शिक्षा के इस पहलू के लिए इस्लामी इतिहास में बहुत-सी शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुईं। इसके लिए पवित्र क़ुरआन में ‘तज़किया’ की शब्दावली अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुई है और एक प्रसिद्ध हदीस में ‘एहसान’ की शब्दावली प्रयुक्त हुई है। यों इन दोनों शब्दों को इकट्ठा करके ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की शब्दावली अपनाई जा सकती है। ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ या इंसान का आध्यात्मिक प्रशिक्षण और आन्तरिक सुधार एक ऐसा विषय है जो आरम्भ से, ताबिईन और तबा-ताबिईन के ज़माने से, न केवल व्यावहारिक, बल्कि ज्ञानपरक दिलचस्पी का विषय रहा है। पिछले सवा चौदह सौ साल में इस विषय पर इस्लाम के इतिहास के बेहतरीन दिमाग़ों ने ग़ौर किया है, और बड़े-बड़े और उच्चतम चरित्र के इंसानों ने इन विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इस विषय पर विद्वानों ने जहाँ विशुद्ध ज्ञानपरक और धार्मिक दृष्टिकोण से चिन्तन-मनन किया, वहाँ हज़ारों विद्वानों ने अपने प्रस्ताव शोध और अनुभवों को लिखित रूप में भी संकलित किया है।
दूसरे विषयों के मुक़ाबले में यह विषय तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। इसलिए कि यह एक ऐसा पहलू है कि जिसका सम्बन्ध अन्य अंगों के मुक़ाबले में इंसान के दिल से अधिक है। यह पहलू विशुद्ध अनुभव, नैतिक रवैये और हार्दिक भावनाओं से अधिक सम्बन्ध रखता है और बोलने से इसका सम्बन्ध कम है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक अनुभूतियाँ और हार्दिक स्थिति अत्यन्त सूक्ष्म और अवर्णीय अनुभव की हैसियत रखते हैं। उनको लेखन का रूप देना आसान काम नहीं। ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ का उद्देश्य इंसानों के चरित्र का सुधार करना है, चरित्र के सुधार के लिए विचारों का सुधार अनिवार्य है।
‘तज़किया’ और ‘एहसान’ वह मैदान है जहाँ बोलने की गुंजाइश कम-से-कम होती है। अत: एक ऐसे विद्यार्थी के लिए जिसका मैदान केवल बोलना हो, विचारों के बारे में बात करना तो किसी हद तक आसान है, लेकिन चरित्र और वह भी हार्दिक चरित्र और हार्दिक अनुभूतियों के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी यह चर्चा केवल उन लेखकों तक सीमित होगी जो इस विषय के बड़े विद्वानों ने संकलित किए हैं और जो पूरब-पश्चिम में, मुस्लिम जगत् के प्राचीन और आधुनिक कालों में, इस मैदान के विशेषज्ञ समझे गए हैं, जिनके लेख, जिनके विचारों के परिणामों और जिनके विचारों ने इंसानों की बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित किया है, और आज भी उनके विचार, न केवल पूरब में बल्कि पश्चिम में भी अत्यन्त महत्त्व और दिलचस्पी के साथ पढ़े जा रहे हैं और इंसानों की दिन-प्रतिदिन संख्या को प्रभावित भी कर रहे हैं।
इसके साथ-साथ इस विषय के मुश्किल होने का एक कारण और भी है, और वह यह है कि इस मैदान में जहाँ इस्लाम के बड़े टीकाकारों और अनुवादकों ने अपने विचार, अध्ययन और अनुभव के परिणाम संकलित किए, वहाँ इस विषय की शब्दावलियाँ को कुछ लोगों ने ग़लत अर्थ भी दिया, कुछ लोगों ने ‘इख़लास’ (निष्ठा) से, लेकिन कम समझ की वजह से ऐसा किया। कुछ लोगों ने निष्ठा और ग़लत समझ से, और कुछ लोगों ने बदनीयती और ग़लत इरादों से ग़लत परिणाम निकालने के लिए इन शब्दावलियाँ का ग़लत प्रयोग भी किया। इन शब्दावलियों का ग़लत प्रयोग करने से ऐसे बदनीयत और बद-अक़ीदा (अन्धविश्वासी) लोगों का उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति था जो इस्लाम या शरीअत के उद्देश्य नहीं थे। चुनाँचे बातिनियों (रहस्यवादियों), क़रामता और इसमाईली धर्म-प्रचारकों ने व्यापक स्तर पर यह काम किया और तसव्वुफ़ की शब्दावलियों के पर्दे में अपने ख़यालात सीधे-सादे मुसलमानों में फैला दिए। इन दो बड़ी मुश्किलों के बावजूद मेरी कोशिश होगी कि ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के विषय पर इस्लामी इतिहास के बड़े विद्वानों और इस मैदान के प्रमाणित प्रवक्ताओं ने जो लिखा है उसका सारांश आपके सामने पेश कर दिया जाए।
सबसे पहली बात जो बड़े सूफ़ियों ने इंसान के सुधार और प्रशिक्षण के सन्दर्भ में महसूस की और जिसको उन्होंने इंसानों के आन्तरिक सुधार में सामने रखना ज़रूरी समझा वह यह है कि इंसान का अस्तित्व एक निहायत व्यापकता रखनेवाला अस्तित्व है। अल्लाह की तमाम सृष्ट रचनाओं में इंसान वह एकमात्र प्राणी है जिसके बारे में कहा गया कि उसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूँकी। और उसको अपने Image पर पैदा किया। यहाँ ‘सूरत’ (Image) से क्या मुराद है, रूह से क्या मुराद है? इसकी बहुत-सी टीकाएँ और व्याख्याएँ हुई हैं। लेकिन इन तमाम व्याख्याओं में जो बात समान है वह यह है कि इंसान का अस्तित्व इतना पेचीदा और इतना असाधारण है कि सृष्टि में किसी और प्राणी का अस्तित्व इतना पेचीदा और असाधारण नहीं। यही वजह है कि इंसान को पूरी तरह समझना जितना मुश्किल है दूसरी चीज़ों को समझना उतना मुश्किल नहीं है।
सृष्टि के रचयिता के बाद सृष्टि का सबसे प्रतिष्ठित अस्तित्व इंसान है। यही वजह है कि इंसान के विभिन्न पहलुओं पर और मानव-जीवन के विभिन्न विभागों पर दार्शनिक और चिन्तक हज़ारों वर्षों से ग़ौर करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक कोई यह नहीं कह सका कि अमुक चिन्तन-व्यवस्था ने या अमुक दार्शनिक या अमुक दर्शन ने इंसान को इस तरह समझ लिया है जिस तरह कि समझने का हक़ है। सम्भवतः यही वजह है कि इस्लामी चिन्तकों ने लिखा था कि जो व्यक्ति अपने आपकी ‘मारिफ़त’ (पहचान) प्राप्त कर ले उसके लिए अल्लाह की ‘मारिफ़त’ (पहचान) प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। अगरचे इस वाक्य को भी ग़लत व्याख्या का निशाना बनाया गया, लेकिन यह वाक्य कहनेवालों का उद्देश्य केवल इतना ही था कि इंसान का अस्तित्व अत्यन्त चिन्तन-मनन की माँग करता है, इसकी वास्तविकता और बारीकी को जानने के लिए बहुत असाधारण सोच-विचार की ज़रूरत है और जब अपने अस्तित्व और सृष्टि के अन्य तथ्यों में सोच-विचार करने का इंसान आदी हो जाए, तो सृष्टि के रचयिता की महानता का एहसास होने लगता है और अल्लाह तआला की क़ुदरत और महानता के असीमित होने का किसी हद तक अन्दाज़ा उसको हो सकता है।
पवित्र क़ुरआन से पता चलता है कि इंसान की तमाम गतिविधियों का दारोमदार, सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में, उसके दिल के ठहराव और आत्मा की पवित्रता पर है। इंसान की हार्दिक अनुभूतियों और आध्यात्मिक भावनाएँ उसकी ज़िन्दगी को सफल भी बनाती हैं और असफल भी बना सकती हैं। अगर ये भावनाएँ और अनुभूतियाँ सही दिशा में काम कर रही हों तो मानव-जीवन सफल रहता है और अगर ये भावनाएँ और अनुभूतियाँ सही दिशा पर काम न कर रही हों तो मानव-जीवन तमाम ज़ाहिरी और भौतिक सफलताओं के बावजूद, तमाम संसाधनों की बहुतायत और साधनों की अधिकता के बावजूद, असफल हो सकता है और हज़ारों बार असफल हुआ है।
यह वही बात है जिसको एक प्रसिद्ध हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैह व सल्लम) ने यों बयान किया है कि “इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा ऐसा है कि अगर वह दुरुस्त रहे तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, और अगर वह ख़राब हो जाए और बिगड़ जाए, या फ़ासिद हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब और फ़ासिद हो जाता है।” निस्सन्देह भौतिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में भी यह बात दुरुस्त है। लेकिन यहाँ इस हदीस का उद्देश्य किसी भौतिक या मनोवैज्ञानिक अर्थ में यह बात कहना नहीं है, बल्कि हदीस का उद्देश्य यह है कि इंसान के कल्याण का मूल आधार उसके दिल की गहराइयों में पैदा होता है। परिवर्तन अच्छा हो या बुरा वह सबसे पहले इंसान के दिल की गहराइयों में जन्म लेता है और जो चीज़ दिल की गहराइयों में जन्म लेती है वह इंसान को और इंसान के आसपास और माहौल को प्रभावित करती है।
इस बात को पवित्र क़ुरआन में एक और आयत में अत्यन्त अर्थपूर्ण ढंग में बयान किया गया है। कहा गया, “अल्लाह उस क़ौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह स्वयं अपने-आपको न बदल ले।” इसका सादा-सा अर्थ यह है कि जब तक इंसान के मन की गहराइयों में कोई ख़राबी पैदा न हो तो वातावरण में ख़राबी पैदा नहीं होती। यह अल्लाह तआला के ‘अद्ल’ के ख़िलाफ़ है कि इंसानों की किसी ख़राबी के बिना, इंसानों की किसी कोताही के बिना, वह उनकी व्यवस्था और उनके माहौल में बिगाड़ पैदा हो जाने की अनुमति दे। दरअस्ल इंसान ख़ुद अपने माहौल में ख़राबी पैदा करता है और ख़राबी का आरम्भ सबसे पहले उसके अन्दर दिल की गहराइयों में होता है।
पवित्र क़ुरआन में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जो चार बड़े कर्त्तव्य बताए गए हैं, उनमें सबसे पहला कर्त्तव्य पवित्र क़ुरआन की आयतें लोगों तक पहुँचाना और पढ़-पढ़कर उनको बताना है। इस महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य के बाद उनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी लोगों का ‘तज़किया’ करना भी है यानी क़ुरआनी आयतें इंसानों तक पहुँचाने के साथ-साथ ये पैग़म्बर इंसानों का ‘तज़किया’ भी करते हैं और अन्दर से इंसानों का आध्यात्मिक सुधार भी करते हैं। आध्यात्मिक सुधार का यह काम मात्र किसी ज़ाहिरी या सरसरी प्रशिक्षण से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि यह एक हमागीर प्रयास का एक हिस्सा है। वह व्यापक प्रयास जिसमें इंसानों के ज़ेहन और सोच का सुधार भी हो, जिसके नतीजे में उनका अन्तर्मन उनके ज़ाहिर के अनुरूप हो जाए। ज़ाहिर (बाहर) में बातिन (अन्दर) की झलक पैदा हो, और ज़ाहिर की ख़ूबियाँ उसके अन्तर्मन में चमक जाती हों। अगर इंसान के ज़ाहिर और बातिन (बाह्य और अन्दर) में टकराव है तो या ज़ाहिर ग़लत रुख़ पर जा रहा है या बातिन ग़लत राह पर चल रहा है, या दोनों ग़लत दिशा में जा रहे हैं।
यह बात कि इंसान को आध्यात्मिक ऊँचाई और क़ल्बी पाकीज़गी (हार्दिक पवित्रता) कैसे प्राप्त हो यह तमाम बड़े-बड़े धर्मों की प्राथमिक दिलचस्पी का विषय रहा है। तमाम बड़े-बड़े धर्मों की गतिविधियों में एक बड़ा मैदान इंसानों का आन्तरिक सुधार भी रहा है। इस विषय पर संसार के धर्मों के बड़े-बड़े चिन्तकों ने हज़ारों वर्ष ग़ौर किया है कि इंसान का आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस तरह किया जाए, और अन्दर से उसका सुधार कैसे किया जाए। मसीहियत, बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म, ये तीन बड़े-बड़े धर्म इस प्रयास में बहुत नुमायाँ हैं। इन तीनों धर्मों के यहाँ mysticism यानी बातिनियत (रहस्यवाद) या दाख़िलियत की परम्परा इतनी लम्बी और इतनी गहरी है कि उसने समय के साथ-साथ एक जटिल दर्शन का रूप ले लिया। एक वैकल्पिक और समानान्तर व्यवस्था के रूप में आख़िरकार दार्शनिकतापूर्ण परम्परा ख़ुद धर्म के मुक़ाबले में आ गई। इस दार्शनिकतापूर्ण परम्परा ने आध्यात्मिकता के नाम पर ‘तफ़ल्सुफ़’ (दर्शनवाद) को बढ़ावा दिया, आध्यात्मिकता के विकास के नाम पर तथ्यों से पलायन की राह अपनाई, धर्म की आत्मा पर कार्यान्वयन के बहाने धार्मिक आदेशों से बचने का रास्ता उपलब्ध किया।
यहाँ इस दर्शन की ख़ूबियों और ख़राबियों के विस्तार में जाना अभीष्ट नहीं। लेकिन इस लम्बी परम्मपरा के अस्तित्व से यह अन्दाज़ा ज़रूर हो जाता है कि इंसानों का आन्तरिक सुधार और आध्यात्मिक चरित्र निर्माण सिर्फ़ इस्लाम का नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले भी विभिन्न धर्मों में बहुत महत्त्वपूर्ण विषय समझा गया।
पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह इन प्रयासों पर टिप्पणी की है और यह बताया है कि ये प्रयास क्यों असफल हुए। इन प्रयासों में असफलता के कारण और तत्त्व क्या थे और जिन कारणों और कारकों से ये प्रयास असफल हुए, उन कारणों और कारकों से मुसलमान कैसे बच सकते हैं। यहूदियों के बारे में क़ुरआन मजीद में बताया गया कि उनका ज़ोर ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़्यादा रहा है। ज़ाहिरी चीज़ों पर ज़ोर की वजह से आन्तरिक सुधार और सच्ची बातें उनकी नज़रों से ओझल हो गईं। यह अतिवाद का एक उदाहरण है। मसीहियत में इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ज़ाहिरी चीज़ों को पूरी तरह अलग कर दिया गया। शुरू से ही ज़ाहिरी चीज़ों को निरस्त कर दिया गया। सेंट पॉल ने तौरात के क़ानून ही को सिरे से निरस्त कर देने से अपने काम का आरम्भ किया। और यों शरीअत की ज़ाहिरी चीज़ों से ताल्लुक़ तोड़ने का फ़ैसला पहले ही दिन कर लिया। फिर आध्यात्मिकता के नाम पर मसीहियत में एक ‘तफ़ल्सुफ़’ (दर्शनवाद) आ गया। जब ज़ाहिरी कामों से सम्बन्ध ख़त्म हो गया तो शरीअत की ज़ाहिरी निशानियाँ एक-एक करके ख़त्म कर दी गईं। शरीअत के क़ानून को पहले दिन निरस्त कर दिया गया। मात्र निरी आध्यात्मिकता जिसका कोई ठोस बौद्धिक और मज़बूत ज्ञानपरक आधार न हो इंसानों के लिए कोई उल्लेखनीय मार्गदर्शन नहीं उपलब्ध कर सकती थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसको एक दर्शन बनना पड़ा और इस ‘तफ़ल्सुफ़’ का नाम मसीहियत की दुनिया में आध्यात्मिकता या mysticism क़रार पाया। इसका नतीजा यह निकला कि दीन (इस्लाम) का यह आध्यात्मिक पहलू ज़िन्दगी और ख़ुद दीन के दूसरे तमाम पहलुओं से दूर होता चला गया। आख़िरकार दोनों में किसी प्रकार की समरूपता शेष न रही। इस पूरी स्थिति का नतीजा यह निकला कि दीन के ज़ाहिरी और आन्तरिक पहलुओं के दरमियान जो परिपूर्णता की कैफ़ियत होनी चाहिए थी, एक-दूसरे के काम आने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, वह पहले दिन से ख़त्म हो गई। पवित्र क़ुरआन ने आध्यात्मिक पवित्रता और दिल की सफ़ाई का जो सबक़ दिया है, जिसके विभिन्न पहलुओं का स्पष्टीकरण हदीसों में किया गया है, उसमें पहले दिन से इस बात का ध्यान रखा गया है कि ज़ाहिरी आदेश और शरीअत के छिपे हुए उद्देश्यों के दरमियान एक सन्तुलन और परिपूर्णता का रंग बरक़रार रहे। जितने परिवर्तन ज़ाहिर में आएँ वे एक वास्तविक हार्दिक परिवर्तन के द्योतक और प्रवक्ता हों। जितने परिवर्तन दिल के अन्दर और आध्यात्मिकता में आते जाएँ उनका इज़हार इंसान के रवैये में व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में होता चला जाए। यह बात इस्लाम की एक विशिष्टता क़रार दी जा सकती है, और बहुत-से अन्य भेदभावों में से एक विशिष्टता यह भी इस्लाम को प्राप्त है कि इस्लाम की शिक्षा में क़ानून की पाबन्दी और शरीअत की ज़ाहिरी चीज़ों से जुड़ाव को आध्यात्मिक श्रेष्ठता का ज़रिया क़रार दिया गया और आध्यात्मिक उच्चता की प्रक्रिया को शरीअत के आदेशों से जुड़ाव से जोड़ दिया गया। इस्लामी इतिहास में जो व्यक्ति जितना ऊँचा ‘वली’ था, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के जितने ऊँचे दर्जे पर आसीन था, वह शरीअत के आदेशों का उतना ही पालन करनेवाला और शरीअत की ज़ाहिरी चीज़ों का उतना ही पाबन्द था। अत: शरीअत की पाबन्दी और आध्यात्मिकता की पूर्ति ये दोनों एक ही शिक्षा के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही मार्गदर्शन ग्रन्थ के दो अध्याय हैं। एक ही वास्तविकता के दो रुख़ हैं, दोनों एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं।
यही वजह है कि इस्लाम में आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता रहित गतिविधियों में वह अन्तर ज़्यादा नुमायाँ नहीं हुआ जो दूसरे बहुत-से धर्मों में पाया जाता है। इस्लाम के अनुसार बहुत-से ऐसे मामलात जो दूसरी जगह विशुद्ध सांसारिक मामले माने जाते हैं, वे इस्लाम में आध्यात्मिक रंग अपना लेते हैं, अगर वे शरीअत की शिक्षा के अनुसार विशुद्ध दीनी भावना से किए जाएँ। इसी तरह ऐसी विशुद्ध आध्यात्मिक क्रियाएँ जो दूसरे धर्मों में केवल आध्यात्मिकता की निशानी समझी जाती हैं, वे इस्लाम में अत्यन्त अप्रिय हो सकती हैं, मज़हब की रूह से दूर क़रार पा सकते हैं, अगर वे शरीअत के उद्देश्यों से हटकर किए जाएँ। इसलिए इस्लाम की शिक्षा में mundane या profane और religious या spiritual का विभाजन अधिक सार्थकता नहीं रखता। ये दोनों एक ही मार्गदर्शन के दो पहलू हैं और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं। परिपूर्णता का यह रंग स्पष्ट रूप से पवित्र क़ुरआन की उन आयतों में सामने आता है जिनमें रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के फ़राइज़ (कर्त्तव्य) बयान किए गए हैं। (देखें सूरा-62, आयत-2) यानी किताब के साथ-साथ तत्त्वदर्शिता और सूझ-बूझ की शिक्षा, तत्त्वदर्शिता और सूझ-बूझ के उद्देश्यों और बुनियादों का अल्लाह की किताब और तत्त्वदर्शिता से रिश्ता जोड़ना यह पैग़म्बर की शिक्षा का और पैग़म्बरी के कर्त्तव्यों का एक बुनियादी हिस्सा है।
हदीसों से भी इस परिपूर्णता के बहुत-से पहलू सामने आते हैं। जो हदीस इस्लाम की सारी आध्यात्मिकता की बुनियाद है, जिससे ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के तमाम दफ़्तर शुरू होते हैं, यह वह हदीस है जिसको ‘हदीसे-एहसान’ भी कहा जाता है और ‘हदीसे-जिब्रील’ भी कहा जाता है। यह हदीस सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और हदीस की कई किताबों में बयान हुई है और बड़े प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने इसको बयान किया है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपनी महफ़िल में बैठे थे। चारों तरफ़ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) बैठे हुए थे, यह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) बयान करते हैं, सहीह बुख़ारी के शब्दों में “एक व्यक्ति अचानक आ गया, जिसके कपड़े अत्यन्त सफ़ेद और बाल अत्यन्त काले थे। हममें से कोई उसे जानता नहीं था। इस बात का ख़ास महत्त्व यों है कि अगर वह मदीने का कोई निवासी होता तो हम सब उसे जानते होते। मुसाफ़िर होता और बाहर से सफ़र करके आया होता तो लिबास, चेहरे और बालों में धूल-मिट्टी लगी होती। सफ़र करने के लक्षण उसके शरीर और लिबास से ज़ाहिर होतें। ज़ाहिर है कि जो मुसाफ़िर ऊँट या घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान में एक महीना सफ़र करके आएगा उसका लिबास भी मैला-कुचैला और धूल-धूसरित होगा। चेहरा पर भी गर्द लगी होगी, और उसके बाल भी धूल में अटे होंगे। शहर का होता तो हम उसे जानते होते। हम उसे जानते भी नहीं थे और सफ़र करके आया हुआ भी मालूम नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आकर बैठ गया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के घुटनों से घुटने मिलाकर बैठा। इसमें से हर चीज़ आश्चर्यजनक थी। इसलिए कि सहाबा इस तरह नहीं बैठते थे। सम्मान से बैठते थे और ज़रा फ़ासला रखकर बैठते थे। फिर कहा कि मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। आप जवाबात दें। इस्लाम क्या है? उसके बारे में मुझे बताइए! नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बताया कि इस्लाम के ये कर्म और ये स्तम्भ हैं। पूछनेवाले ने कहा, आप सही कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) फ़रमाते हैं हमें इसपर आश्चर्य हुआ कि सवाल भी कर रहा है और पुष्टि भी करता है। अगर सवालों के जवाबात मालूम थे, तो पूछे क्यों? और अगर जवाबात मालूम नहीं थे तो पुष्टि क्यों और किस आधार पर की? सवाल जवाब के इस सिलसिले में अजनबी ने महत्त्वपूर्ण सवाल तीन पूछे। एक पूछा कि इस्लाम क्या है? जिसके जवाब में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस्लाम के कर्मों और स्तम्भों का ज़िक्र किया, पाँच स्तम्भ, यानी कलिमए-शहादत और चारों इबादतों का ज़िक्र किया। यानी ज़ाहिरी आदेशों को बयान किया। ईमान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने अक़ीदे बयान किए। फिर पूछा ‘एहसान’ क्या है? जो तीन हिस्से शरीअत के मैंने पहले रोज़ की चर्चा में बताए थे वे तीनों इस हदीस में मौजूद हैं।
जब ‘एहसान’ का सवाल किया तो उसे जवाब मिला। ‘एहसान’ यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो, इसलिए कि अगर तुम उसको नहीं देख रहे तो वह तो तुम्हें देख रहा है। यह यक़ीन और उसके सामने हाज़िरी का यह पूरा आभास पैदा करना ही ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस आभास को पैदा करने के लिए लम्बा प्रशिक्षण दरकार है, फिर उसको बरक़रार रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है।
यह एहसास जब पूरे तौर पर जाग्रत हो जाए और इंसान हर समय और हर पल अपने दिल की गहराइयों से यह महसूस करता रहे कि मैं लगातार अल्लाह की नज़रों में हूँ, अल्लाह तआला की आँख लगातार मुझे देख रही है तो इससे यक़ीन और ईमान की कैफ़ियत ही और हो जाती है। इस समझ और विश्वास के साथ जब इबादत की जाएगी तो उसकी कैफ़ियत ही कुछ और होगी। इस कैफ़ियत को ‘एहसान’ कहते हैं। इस कैफ़ियत का अस्ल और स्तरीय दर्जा तो यह है कि इंसान अपनी श्रद्धा की आँख से, ईमान की आँख से और अन्तर्दृष्टि से अल्लाह को देख रहा हो। अल्लाह की सच्चाइयों को समझ रहा हो, लेकिन अगर समझने का स्तर वह न हो तो कम-से-कम विश्वास का इतना स्तर होना चाहिए कि इंसान यह महसूस करे कि मैं लगातार अल्लाह की नज़रों में हूँ। यह एहसास उसी समय हो सकता है जब दिलों की सफ़ाई और आध्यात्मिक पवित्रता एक विशेष स्तर पर पहुँच गई हो। दिलों का ‘तज़किया’ इतना हो चुका हो कि इंसान के दिल में ग़लत ख़यालात और अनुभूतियाँ पैदा न हों। यह बात कि ज़ाहिर में तो नमाज़ अदा हो रही है और ज़ेहन में बैंक बैलेंस का हिसाब हो रहा है, या बज़ाहिर तो नमाज़ की क्रियाएँ हो रही हैं, और वास्तव में नौकरी की सुविधाओं और शर्तों का निर्धारण हो रहा है। यह रवैया अल्लाह के सामने हाज़िर होने के एहसास के ख़िलाफ़ है। इस तरह के और भी बहुत-से मामलात हो सकते हैं जहाँ विशुद्ध इबादत में सांसारिक ख़राबियाँ शामिल हो जाती हों।
जब किसी इंसान की नैतिक स्थिति का सुधार हो चुका हो और उसके नैतिक प्रशिक्षण का स्तर दरकार स्तर तक पहुँच चुका हो तो उसके प्रभाव अवश्य ही इंसान के रवैये और कार्य-नीति में ज़ाहिर होते हैं। दूसरे इंसानों से सम्पर्कों के मामले में और सृष्टि के रचयिता के साथ अपने सम्बन्ध बारे में इंसान का रवैया परिवर्तित होने लगता है। जब ये तीनों अपेक्षाएँ पूरी हो जाती हैं, यानी दिल की सफ़ाई भी, दिलों का ‘तज़किया’ भी और नैतिकता की पवित्रता भी तो इन सबके समष्टीय परिणाम के तौर पर वह कैफ़ियत सामने आ जाती है जिसको हदीस में ‘एहसान’ के शब्द से याद किया गया है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के समय में उनके प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) उनके प्रशिक्षण से इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया करते थे। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के बारे में यह समझना दुरुस्त नहीं है कि उनमें सबका आध्यात्मिक दर्जा और स्थान एक ही था, या प्रशिक्षण की दृष्टि से, या ‘तज़किया’ की दृष्टि से सब सहाबा एक ही दर्जे पर आसीन थे। इससे कोई भी मतभेद नहीं कर सकता कि प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में जो दर्जा हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ को प्राप्त था वह दूसरों का नहीं था। यह एक निश्चित बात है कि जो दर्जा शेष तीनों ख़लीफ़ाओं का था या अशरा-मुबश्शरा (वे दस भाग्यशाली सहाबी जिन्हें उनकी ज़िन्दगी में ही उनके जन्नती होने की शुभसूचना दे दी गई थी) का था, वह बहुत-से दूसरे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का नहीं था। फिर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में कुछ लोग वे भी थे जिनको प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रशिक्षण में रहने का संयोग प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से केवल मुलाक़ात की और केवल संक्षिप्त मुलाक़ात में उनके हाथ पर इस्लाम स्वीकार किया, और उसके बाद अपने-अपने इलाक़ों को वापस चले गए और प्रशिक्षण के लिए उनको दूसरे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के मार्गदर्शन के तहत काम करना पड़ा। इसलिए प्रशिक्षण के दर्जों में और दिलों की सफ़ाई के दर्जों में जिस तरह का अन्तर प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के मध्य पाया जाता था वह आइन्दा भी ईमानवालों के दरमियान मौजूद रहेगा और हमेशा रहेगा।
यह बात कि हर व्यक्ति को हर समय और बेहतर-से-बेहतर दर्जों और मरतबों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, इस्लामी आध्यात्मिकता के इतिहास में एक विशिष्ट लक्ष्य की हैसियत रखती है। यह बात सहाबा के ज़माने में भी आम थी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) समय-समय पर इस ज़रूरत का एहसास किया करते थे कि ईमान में और शिद्दत और विश्वास में और परिपक्वता की प्राप्ति के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब तक ज़िन्दा थे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनकी मजलिस में जाया करते थे और आध्यात्मिक प्रशिक्षण और स्थानों की और ऊँचाइयों पर आसीन होकर आया करते थे। यह प्रसिद्ध घटना हममें से हर एक ने पढ़ी और सुनी है कि एक प्रसिद्ध सहाबी हज़रत हंज़ला (रज़ियल्लाहु अन्हु) एक बार घर से परेशानी के आलम में निकले, रास्ते में देखा कि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) जा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ ने उनके चेहरे पर परेशानी के लक्षण देखकर पूछा कि “हंज़ला कहाँ जा रहे हो?” जवाब दिया कि “मुझे तो लगता है कि मैं मुनाफ़िक़ (मिथ्याचारी) हो गया हूँ।” पूछा, “क्या बात है?” बताया कि “जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की महफ़िल में होता हूँ तो रंग और होता है और ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह तआला मुझे देख रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन जब घर वापस जाता हूँ, दुकान, कारोबार, व्यापार, और घर-बार की व्यस्तताओं में रहता हूँ तो उस समय यह कैफ़ियत नहीं रहती।” गोया दोनों कैफ़ियतों में यह फ़र्क़ उनको ‘निफ़ाक़’ (मिथ्याचार) का एक अंग महसूस हुआ। हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया कि “यह कैफ़ियत तो मुझे भी महसूस होती है। अगर यह निफ़ाक़ है तो बड़ी बुरी बात है। चलो चलकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछते हैं।” दोनों लोगों ने आकर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने समस्या बयान की। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तसल्ली दी और फ़रमाया कि यह कोई निफ़ाक़ नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक बात है। इस घटना से यह ज़रूर अन्दाज़ा होता है कि आध्यात्मिक दर्जों में कमी-बेशी की अनुभूतियाँ प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) को भी पेश आया करती थीं और आध्यात्मिक दर्जों में और बेहतरी की ज़रूरत सहाबा के क्षेत्रों में भी समय-समय पर महसूस की जाती थी।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) एक-दूसरे की मजलिस से लाभान्वित हुआ करते थे। ये उदाहरण हदीस की कितबों में मिलते हैं कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से फ़रमाया, “आओ थोड़ी देर एक साथ बैठो, ताकि इस तरह साथ बैठकर हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकें।” यह बात प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) एक-दूसरे से कहा करते थे। इसलिए जब तक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ज़िन्दा रहे उस समय तक उनका विशेष रूप से बड़े और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का अस्तित्व एक पारस पत्थर था, जो उनमें से किसी के जितना क़रीब आया वह इतना ही चमक गया, लेकिन समय के साथ-साथ जहाँ बड़े सहाबा दुनिया से विदा होते गए वहाँ बड़े पैमाने पर सांसारिक सुविधाओं और भौतिक सुखों को भी बढ़ावा मिला। भौतिक संसाधनों और धन-सम्पत्ति में भी वृद्धि हुई। धन-दौलत की कसरत की वजह से ऐसे हालात भी पैदा हुए जिनमें इंसान से कभी-कभी उच्च आध्यात्मिक दर्जों और नैतिक पवित्रता की उच्च उद्देश्यों से मानव दुर्बलताओं के कारण उपेक्षा हो सकती है। इन हालात में एक पूर्ण और व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था की ज़रूरत पेश आई, पूर्ण और व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए पहले चरण के तौर पर उन तमाम निर्देशों और मार्गदर्शन को संकलित किया जाना ज़रूरी था जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के द्वारा प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के द्वारा और बड़े ताबिईन के द्वारा सामने आई थी। क़ुरआन की टीका करने की कला संकलित हुई, इल्मे-हदीस संकलित हुआ, फ़िक़्ह संकलित हुई, कलाम संकलित हुआ, तो तज़किए और प्रशिक्षण की व्यवस्था संकलित होने में क्या चीज़ रुकावट थी। चुनाँचे बड़े मुहद्दिसीन ने ज़ुह्द, रिक़ाक़, तरग़ीबो-तरहीब और प्रतिदिन के विर्द और अज़कार के विषयों से सम्बन्धित हदीसों के संग्रह तैयार किए। यह इल्मे-तसव्वुफ़ के संकलन की तरफ़ पहला क़दम था। जल्द ही ‘तज़किया’ और प्रशिक्षण के आदाब भी संकलित हुए।
जब कोई चीज़ कलात्मक रूप से संकलित होती है, जब किसी ज्ञान के तथ्यों को ज्ञानपरक दृष्टि से संकलित किया जाता है तो उस ज्ञान के तथ्यों एवं धारणाओं को दूसरे ज्ञान के तथ्यों और धारणाओं से अलग करने के लिए शब्दावलियाँ ख़ुद-ब-ख़ुद सामने आ जाती हैं। शब्दावलियाँ इल्मे-तफ़सीर (क़ुरआन की टीका का ज्ञान) में भी सामने आईं। इल्मे-तफ़सीर की शब्दावलियाँ सहाबा के ज़माने में न थीं। इल्मे-हदीस की बहुत-सी शब्दावलियाँ सहाबा और ताबिईन के ज़माने में नहीं थीं। यही हाल फ़िक़्ह और इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की शब्दावलियाँ का है। ये सब शब्दावलियाँ बाद में अस्तित्व में आई हैं। तसव्वुर पहले सामने आता है, वास्तविकता पहले अस्तित्व में आती है शब्दावलियाँ बाद में बनती हैं। इसलिए तमाम ज्ञान-विज्ञान की शब्दावलियों को नज़रअन्दाज़ करके केवल तसव्वुफ़ या प्रशिक्षण की शब्दावली के बारे में यह कहना कि चूँकि अमुक शब्दावली नबी के ज़माने में नहीं थी अत: वह तसव्वुर जिसकी वह शब्दावली निशानदेही करती है वह धारणा भी ग़ैर-इस्लामी है, दुरुस्त नहीं है। अगर किसी शब्दावली का नया होना किसी धारणा के अस्वीकार्य होने के लिए काफ़ी दलील है तो इसकी चोट इस्लामी ज्ञान-विज्ञान में हर ज्ञान पर पड़ेगी।
[यहाँ लेखक को समझने में ग़लती हो रही है। इल्मे-हदीस और तफ़सीर आदि के लिए जो शब्दावलियाँ इस्तेमाल हुईं उनकी ज़रूरत भाषा और व्याकरण की दृष्टि से थी, ताकि बाद के लोगों को समझने में आसानी हो। इन शब्दावलियों से इस्लाम की मूल धारणाओं में किसी प्रकार का बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। इसके विपरीत तसव्वुफ़ के नाम पर जो नई शब्दावलियाँ और नए-नए तरीक़े अस्तित्व में आए, वे केवल समझने-समझाने तक सीमित न रहे, बल्कि बाक़ायदा एक अलग ज्ञान के रूप में जाने-जाने लगे और यही नहीं, बल्कि उनके द्वारा इस्लामी अक़ीदों (धारणाओं) के बिल्कुल विरुद्ध अक़ीदे क़ायम कर लिए गए। इसलिए तसव्वुफ़ में दाख़िल नए तरीक़ों और शब्दावलियों की इल्मे-हदीस, इल्मे-फ़िक़्ह और इल्मे-तफ़सीर जैसी शब्दावलियों से तुलना करना और उन्हें उन्हीं के समान क़रार देना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है——— अनुवादक]
दूसरी बात जो बहुत-से लोगों को ग़लत-फ़हमी में डालती है वह कुछ सूफ़ियों के ऐसे बयानात हैं जो इस्लामी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं हैं। ‘तज़किया’ और तसव्वुफ़ के विशाल भंडार में ऐसे बयानात भी मिलते हैं जो शरीअत की शिक्षा, परम्पराओं या आत्मा से टकराते हैं, लेकिन सच यह है कि ‘इल्मे-तज़किया’ या ‘इल्मे-एहसान’ का ऐसे बयानात से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनमें से अधिकांश बयानों को विभिन्न बुज़ुर्गों से जोड़ने की बात भी सन्दिग्ध है।
[यहाँ भी लेखक का कहना दुरुस्त नहीं है। तसव्वुफ़ की जिन किताबों (या बयानों) के बारे में वे कह रहे हैं कि वे सन्दिग्ध हैं, वे किताबें (और बयानात) आज भी छप रही हैं और उनके उन्हीं लेखकों के नाम से छप रही हैं, जिनके बारे में लेखक महोदय कहते हैं कि उनसे उनका जोड़ना सन्दिग्ध है। अगर ऐसा ही है तो या तो उन सन्दिग्ध बयानोंवाली किताबों का प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए या फिर उनमें से वे सन्दिग्ध बयानात छाँटकर निकाल देने चाहिएँ। मगर इन दोनों कामों में से एक भी नहीं किया जा रहा है। तसव्वुफ़ को इस्लाम समझनेवाले इन किताबों की सारी बातों को दुरुस्त मानते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग एतिराज़ करते हैं तब ऐसी बातें बनाई जाती हैं जैसी ये लेखक महोदय कर रहे हैं। आगे भी आपको इस तरह की तावीलात मिलंगी।——— अनुवादक]
ऐसे कमज़ोर बयानात मुफ़स्सिरीन के यहाँ भी कसरत से मिलते हैं। बहुत-से मुफ़स्सिरीन ने इसराईली उल्लेख तफ़सीरों में नक़्ल कर दिए हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। इल्मे-हदीस का इतिहास, हदीस गढ़ने के फ़ित्ने और गढ़नेवालों की हरकतों को जानते हैं। हदीस के इतिहास का हर विद्यार्थी हदीस गढ़ने के फ़ितने के विवरणों से किसी-न-किसी हद तक परिचित है। प्रतिष्ठित फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) और उलमाए-उसूल अगरचे बड़ी हद तक इससे बचे रहे, लेकिन उनमें भी कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बहसें और समस्याएँ उठाईं जिनका प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध फ़िक़्ह, उसूले-फ़िक़्ह और शरीअत से नहीं था। यही हाल दार्शनिकों का है, दार्शनिकों के नाम से जहाँ बहुत-से सही विचारोंवाले और सन्तुलित प्रकार के लोग सामने आए वहाँ कुछ ग़लत प्रकार के लोग, ज़िंदीक़ और मुल्हिदीन (नास्तिक) भी सामने आए। इसलिए सही-ग़लत के इस संग्रह में किसी चीज़ को समझने का या जानने का सही तरीक़ा यह है कि उसको उसकी अस्ल बुनियादों की रौशनी में और प्रमाणित और बड़े व्याख्याताओं के लेखों की रौशनी में समझा जाए। जिन लोगों ने ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के मैदान में शरीअत के आदेशों और शिक्षा का पूरे तौर से ध्यान रखा और तमाम सम्बन्धित धारणाओं और शब्दावलियाँ की वे व्याख्याएँ और टीकाएँ कीं जो शरीअत के उद्देश्यों की पूर्ति करती हों और शरीअत की शिक्षा की दृष्टि से स्वीकार्य हों, तसव्वुफ़ को समझने के लिए ऐसे ही प्रमाणित विद्वानों के कलाम और सन्देश से लाभ उठाया जाना चाहिए। ‘तज़किया’ और आध्यात्मिकता के मामले में जो कुछ बड़े विद्वानों ने कहा है उसी को इस्लामी दृष्टिकोण का प्रमाणित प्रवक्ता और स्वीकार्य नुमाइंदा क़रार दिया जाना चाहिए। इमाम ग़ज़ाली, शैख़ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, अवारिफ़ुल-मआरिफ़ के लेखक, अल्लामा इब्ने-क़य्यिम, मुजद्दिद अल्फ़सानी, अल्लामा अब्दुल वह्हाब शेरानी, हज़रत अली हजवेरी जैसे बुज़ुर्ग ही तसव्वुफ़ के अस्ल नुमाइंदा और प्रवक्ता हैं।
[ज्ञात रहे कि अली हजवेरी की किताब ‘कशफ़ुल-महजूब’ जो तसव्वुफ़ की बहुत प्रसिद्ध किताब है और अत्यन्त प्रमाणित मानी जाती है, उसमें ख़ुद बहुत-सी बातें इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध हैं——— अनुवादक]
यहाँ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के नाम से ग़लत-फ़हमी न पैदा होनी चाहिए। इस नाम के दो व्यक्ति हैं। एक फ़ल्सफ़ी (दार्शिनक) थे जिनके बारे में उन्हीं के ज़माने के कुछ लोगों का ख़याल था कि उनके ख़यालात इस्लाम के विरुद्ध हैं और उनके लेखों में इस्लाम से विमुखता अपनाई गई है। उस ज़माने की हुकूमत ने उन्हें नास्तिकता के अपराध में सज़ा-ए-मौत दे दी थी। क़त्ल किए गए यह शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जो इशराक़-दर्शन के संस्थापक थे, यह उन शहाबुद्दीन सुहरवर्दी से भिन्न हैं जो प्रसिद्ध सिलसिला-ए-तसव्वुफ़ के संस्थापक थे। जिनसे हज़रत ख़्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का सम्बन्ध था जो हमारे उपमहाद्वीप के बड़े सूफ़ियों में से थे। हज़रत शैख़ अली हजवेरी वह हैं जिनकी किताब ‘कशफ़ुल-महजूब बहुत प्रसिद्ध है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, शैख़ अहमद सरहिन्दी के मक्तूबात (पत्र) तसव्वुफ़ के पूरे इतिहास में बहुत नुमायाँ स्थान रखते हैं। उपमहाद्वीप के शैख़ अब्दुल-हक़ मुहद्दिस देहलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का दर्जा भी आध्यात्मिकता और ‘तज़किया’ और ’एहसान’ के मैदान में बहुत ऊँचा है। ये और इन जैसे दूसरे लोग वे हैं, जिन्होंने क़ुरआन और सुन्नत की अस्ल शिक्षा को सामने रखते हुए आध्यात्मिक ‘तज़किया’ और नैतिक प्रशिक्षण के सिद्धान्त बयान किए हैं। इन लोगों ने तसव्वुफ़ की शब्दावलियों की जो व्याख्याएँ की हैं वे क़ुरआन और सुन्नत के अनुसार स्वीकार्य हैं, इन व्याख्याओं का आधार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की प्रशिक्षण विधि पर है।
कुछ लोगों का यह तर्क और इसपर आग्रह कि ‘तसव्वुफ़’ का शब्द चूँकि इस्लाम के मुख्य दौर के इतिहास में प्रचलित नहीं था अत: तसव्वुफ़ के नाम से जो कुछ मौजूद है वह सारा-का-सारा रद्द करने लायक़ है, यह कोई ज्ञानपरक तर्क नहीं है। यह शब्दावली अगर सहाबा के ज़माने में नहीं थी तो ताबिईन और तबा-ताबिईन के ज़माने में अस्तित्व में आ चुकी थी। ज़ाहिद पश्मीना पोश के लिए सूफ़ी की शब्दावली ताबिईन के आख़िरी ज़माने के तुरन्त बाद प्रचलित हो गई थी। ताबिईन का आख़िरी ज़माना और तबा-ताबिईन का ज़माना वह है जब अल्लाह तआला ने बहुत विशाल स्तर पर मुसलमानों को सांसारिक धन-दौलत प्रदान की। बनी-उमय्या, बनी-अब्बास की बड़ी-बड़ी अज़ीमुश्शान हुकूमतें क़ायम हुईं। और सांसारिक संसाधनों और भौतिक साधनों की दृष्टि से मुसलमानों पर तरह-तरह की नेमतों के दरवाज़े खुल गए। हर प्रकार की दौलत की अधिकता से एक वर्ग में भौतिकवाद का सैलाब आता महसूस हुआ। इस भौतिकवाद के सैलाब में कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि अगर इस्तिग़ना (दुनिया के प्रति निस्पृहता) और ज़ुह्द (संयम) की शिक्षा को आम न किया गया, तो आगे चलकर लोग भूल जाएँगे कि शरीअत में ज़ुह्द और इस्तिग़ना की शिक्षा भी थी। शरीअत में ‘तौबा’ की शिक्षा भी थी, प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में कुछ अत्यन्त मुस्तग़नी (निस्पृह) और ज़ाहिद (संयमी) स्वभाव के लोग भी थे। इसलिए मुस्लिम समुदाय के कुछ नेक और भले लोगों ने ज़ुह्द और इस्तग़िना, तौबा और अल्लाह के ज़िक्र का सबक़ नए सिरे से याद दिलाया। उन्होंने ज़ुह्द और इस्तिग़ना के सिद्धान्तों पर न केवल मौखिक रूप से ज़ोर दिया, बल्कि अपने तर्ज़े-अमल से भी अत्यन्त सादगी का एक ऐसा रवैया अपनाया जिसकी सीमाएँ कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को ही देखनेवालों को संन्यास से मिलती हुई महसूस होती हैं। इस सादगी के रवैये को अपनानेवाले हर तरह के लोग थे। उनमें कुछ आधुनिकतम विद्वान भी शामिल थे, और ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपने-आपको केवल नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण तक सीमित रखा। चूँकि यह लोग बहुत सादा खाना खाते, मोटा-झोटा कपड़ा पहनते, इसलिए ये लोग सादगी में नुमायाँ होते चले गए। सादा और मोटे कपड़े की वह क़िस्म जो इन दिनों प्रचलित थी उसको ‘सूफ़’ कहा जाता था। इसलिए बहुत जल्द सूफ़ पहनने के लिए तसव्वुफ़ की शब्दावली भी प्रचलित हो गई। यानी वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा और इरादे से सूफ़ का कपड़ा प्रयोग करता है और सादगी को एक जीवन-प्रणाली के तौर पर अपनाता है।
लेकिन तसव्वुफ़ की शब्दावली का यह अर्थ नहीं है कि यही वह एकमात्र शब्दावली थी जो इस दौर में या बाद के समयों में प्रयुक्त हुई। उसके लिए फ़िक़्हुन-नफ़्स की शब्दावली भी कुछ बड़े इस्लामी विद्वानों ने प्रयोग की है। ‘अल-फ़िक़्हुल-अकबर’ में हज़रत इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) ने जहाँ कलाम की समस्याओं से बहस की है वहाँ आध्यात्मिकता और तज़किए की समस्याओं का भी ज़िक्र किया है। ‘फ़िक़्हुल-क़ल्ब’ की शब्दावली भी कुछ बुज़ुर्गों ने प्रयोग की है। ‘फ़िक़्हुन-नफ़्स’ और ‘फ़िक़्हुल-बातिन’ की शब्दावलियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं और जैसा कि कहा गया है कि “शब्दावली में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।” अस्ल महत्त्व शीर्षक को नहीं उसमें बयान बातों को प्राप्त होता है। तसव्वुफ़ का विस्तृत विवरण क्या है? अगर वह शरीअत के अनुसार है, अगर वह शरीअत के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, अगर उसकी वजह से शरीअत के आदेशों पर अमल करने की दिलचस्पी पैदा होती है, तो वह निस्सन्देह शरीअत में अभीष्ट हैं। शीर्षक ‘फ़िक़्हुन-नफ़्स’ हो या ‘फ़िक़्हुल-बातिन’ हो, या ‘फ़िक़्हुल-क़ल्ब’ हो, यह वह चीज़ है जो शरीअत में अभीष्ट और दरकार है। शरीअत ने दिल के सुधार के लिए जो शिक्षा दी है, उसके ज्ञानपरक क्रम ही का नाम तसव्वुफ़ है।
पवित्र क़ुरआन में और हदीस में एक महत्त्वपूर्ण विषय बयान हुआ है और विभिन्न अन्दाज़ से बयान हुआ है। शरीअत ने बार-बार यह प्रेरणा दिलाई है कि इंसान अपने-आपको अल्लाह के निकट करे। अल्लाह से मुलाक़ात के लिए अपने को तैयार करे। इस निकटता को पवित्र क़ुरआन ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न ढंग से बयान किया है। “हम शहेरग से भी ज़्यादा इंसानों के क़रीब हैं।” यह निकटता जिसकी पवित्र क़ुरआन ने शिक्षा दी है इससे मुराद निश्चय ही कोई ज़ाहिरी या भौतिक या शारीरिक निकटता नहीं है। यह एक ऐसे एहसास और आभास का नाम है, यह एक ऐसा निकटता का आभास है जिसको आप आध्यात्मिक निकटता कह सकते हैं। यही वजह है कि कुछ हदीसों से यह मालूम होता है कि इंसान अल्लाह तआला की निकटता का सबसे ऊँचा दर्जा जब प्राप्त करता है जो वह सजदे की हालत में हो। क़ुरआन से भी इस का समर्थन होता है। “सजदा करो और उसकी निकटता प्राप्त करो।” (क़ुरआन, 96:19) यहाँ जिस निकटता का ज़िक्र है वह निस्सन्देह आध्यात्मिक और आभासी निकटता है।
‘क़ुर्ब’ (निकटता) के साथ-साथ पवित्र क़ुरआन ने ‘लिक़ा’ या अल्लाह से मुलाक़ात की शब्दावली भी प्रयोग की है। “जो व्यक्ति यह इच्छा रखता हो कि अल्लाह से मान-सम्मान के साथ मुलाक़ात करे तो फिर वह नेक काम भी करे।” (क़ुरआन, 18:110) एक और जगह कहा गया है “हर तरफ़ से मुँह मोड़कर सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ रुख़ कर लो, हर किसी से तोड़कर अल्लाह से जोड़ो।” (क़ुरआन, 73:8) ये और इस तरह की अनगिनत आयतें किसी शारीरिक या भौतिक अर्थ में अल्लाह की निकटता को बयान नहीं करतीं। यह एक ऐसे ‘क़ुर्ब’ (निकटता) को बयान कर रही हैं जिसको हम विशुद्ध आध्यात्मिक या आभासी निकटता क़रार दे सकते हैं। हदीस में कहा गया है “जो अल्लाह से मुलाक़ात को पसन्द करता है अल्लाह तआला भी उससे मुलाक़ात को पसन्द करता है।” यह ‘लिक़ा’ या मुलाक़ात क्या है? ज़ाहिर है प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने, ताबिईन ने और तबा-ताबिईन ने इस ‘लिक़ा’ और ‘क़ुर्ब’ की प्राप्ति के लिए हर सम्भव कोशिश की। इस कोशिश के विवरण को जानना और उससे लाभ उठाना बादवालों के लिए अनिवार्य है। उन्हीं विवरणों को जानने, उनको इल्मी अन्दाज़ में संकलित करने और उनकी रौशनी में प्रशिक्षण के नियमों और सिद्धान्त संकलित करने ही को तसव्वुफ़ को शब्दावली से याद किया गया। पवित्र क़ुरआन ने इस ‘क़ुर्ब’ की प्राप्ति के लिए इंसानों को अल्लाह की तरफ़ दौड़ने की भी शिक्षा दी है। “दौड़कर अल्लाह की तरफ़ जाओ।” अगर इस दौड़ से कोई शारीरिक दौड़ मुराद नहीं है, और निश्चय ही मुराद नहीं है, तो यह सवाल अनिवार्य रूप से पैदा होता है कि इंसान अल्लाह की तरफ़ कैसे दौड़े? मैं अगर अल्लाह की तरफ़ दौड़कर जाना चाहूँ तो मुझे पहले यह जानना चाहिए कि कहाँ से दौड़ूँ और दौड़कर कहाँ जाऊँ। ज़ाहिर है, मैं यहाँ जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से दौड़कर जाऊँ तो कहाँ जा सकता हूँ, अल्लाह तआला किसी निर्धारित जगह पर physical अर्थ में तो मौजूद नहीं है कि मैं दौड़कर वहाँ चला जाऊँ और मान लीजिए अगर उसका शारीरिक अस्तित्व किसी सीमित जगह में मान भी लिया जाए (जैसा कि कुछ ज़ाहिर-परस्त और सीधे-सादे लोगों का आग्रह रहा है) तो मैं दौड़कर वहाँ नहीं जा सकता। अत: यहाँ दौड़ने से मुराद इसके सिवा कुछ नहीं है कि भौतिकवाद की गन्दगियों से बचकर दौड़ो, दुनिया और धन-दौलत की चाह में डूब जाने से दौड़ो, पाशविक भावनाओं और इच्छाओं से दौड़ो। पाशविक भावनाओं और पाशविकता से दौड़कर अलग हो जाओ, और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ो जहाँ से अल्लाह का ‘क़ुर्ब’ प्राप्त हो। इसका यही अर्थ है, इसके अलावा इस जगह और कोई अर्थ क़रार नहीं दिया जा सकता। जब इंसान दौड़ने की इस राह पर चल पड़ता है और अल्लाह के ‘क़ुर्ब’ का आला और बरतर मर्तबा या मरहला उसका अभीष्ट बन जाता है तो फिर आख़िरकार एक मरहला ऐसा आना चाहिए कि उसको अल्लाह के ‘क़ुर्ब’ की दरकार मंज़िल प्राप्त हो जाए। यही वह मरहला है जिसे कुछ सूफ़िया की ज़बान में ‘वुसूल’ के शब्द से याद किया गया। यानी अल्लाह तक वह पहुँच गया, अल्लाह का ‘क़ुर्ब’ इसे प्राप्त हो गया और जो मंज़िले-मक़्सूद थी वह उसको प्राप्त हो गई।
[यहाँ फिर लेखक महोदय ने तसव्वुफ़ की ख़राबी को छिपाने का प्रयास किया है। इस्लाम में यह अभीष्ट ही नहीं है कि कोई व्यक्ति इसी दुनिया में अल्लाह के ‘क़ुर्ब’ का सर्टिफ़िकेट प्राप्त कर ले, बल्कि ऐसा करना सम्भव भी नहीं है। इस्लाम तो हर इंसान से सारी ज़िन्दगी अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने और इसके द्वारा उसका ‘क़ुर्ब’ प्राप्त करने की अपेक्षा करता है और बताता है कि यह प्रयास व्यक्ति को अपनी मौत तक जारी रखना है, और इसमें वह कितना सफल हुआ इसका परिणाम उसे मरने के बाद आख़िरत में ही मालूम होगा। दुनिया में वह सही रास्ते पर है या नहीं इसे जानने के लिए उसे बस यह देखना होगा कि वह क़ुरआन एवं सुन्नत के अनुसार अपना जीवन गुज़ार रहा है या नहीं। किसी व्यक्ति ने इसी दुनिया में अल्लाह का ‘क़ुर्ब’ प्राप्त करके ‘वस्ल’ (ख़ुदा से मिल जाने) का स्थान पा लिया, यह केवल सूफ़ियों का मनगढ़न्त ख़याल है, इस्लामी शिक्षाओं का हिस्सा नहीं———अनुवादक]
पवित्र क़ुरआन ने एक आयत में दो अत्यन्त व्यापक शब्द प्रयुक्त किए हैं जिनसे ‘अस्हाबे-तज़किया’ और ‘अस्हाबे-एहसान’ ने दो बड़ी शैलियाँ निकाली हैं। एक आयत है जिसमें कहा गया है कि “जिसको अल्लाह चाहता है चुनकर अपना ख़ास कर लेता है और जो उसकी तरफ़ वापस लौटना चाहता है अल्लाह तआला उसको रास्ता बता देता है।” (क़ुरआन, 42:13) इस आयत की व्याख्या में कुछ बड़े प्रशिक्षकों ने लिखा है कि ‘वुसूल’ और ‘लिक़ा’ के मामले में इंसानों की दो क़िस्में हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको किसी रास्ते को काटने या बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तआला ख़ुद उनको चुन लेता है और रहमत ख़ुदावंदी और अपनी कृपा से अचानक या बहुत जल्द उनको उसकी निकटता प्राप्त हो जाती है। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस रास्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लम्बे प्रशिक्षण से गुज़रना पड़ता है। यह सिर्फ़ और केवल अल्लाह तआला की मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि किसी को मेहनत के बिना मंज़िले-मक़्सूद तक पहुँचा देता है और कुछ को प्रशिक्षण की कठिन मंज़िल सर करनी पड़ती है। इन दोनों रास्तों में से एक को शब्दावली में ‘सुलूक’ से याद किया गया, दूसरे को शब्दावली में ‘जज़्ब’ से याद किया गया। अत: ये दो रास्ते ख़ुद पवित्र क़ुरआन से साबित हैं, इन दोनों रास्तों या शैलियों के लिए शब्दावली जो भी प्रयोग की जाए वह महत्त्वहीन बात है।
[यह भी क़ुरआन से ग़लत मतलब निकाला गया है। अल्लाह के चुने हुए बन्दे होने का सर्टिफ़िकेट केवल पैग़म्बरों को मिला है, उसके बाद बेहतरीन लोग नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सहाबा हैं। उनके बाद किसी के बारे में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अल्लाह की निकटता प्राप्त कर ली है या उसे अल्लाह से ‘वस्ल’ प्राप्त हो गया है। ऐसे दावे सिर्फ़ झूठे दावे हैं। इस्लाम के निकट दुनिया केवल परीक्षा-स्थल है, न कि परिणाम-स्थल भी। परिणाम जो भी होगा वह केवल आख़िरत में सामने आएगा। कोई कितनी भी तपस्या कर ले, अपना पारलौकिक परिणाम यहाँ नहीं जान सकता न यह निश्चित कर सकता है कि बस अब वह अल्लाह का निकटवर्ती और प्रिय बन्दा बन चुका है———अनुवादक]
अभी मैंने बताया था कि बुख़ारी और मुस्लिम दोनों की प्रसिद्ध रिवायत है जिसमें दिल की सलाह (सुधार) और दिल के फ़साद (बिगाड़) को पूरी ज़िन्दगी का सुधार और पूरी ज़िन्दगी का बिगाड़ कहा गया है। दिल के सुधार के लिए जहाँ शिक्षा-प्रशिक्षण दरकार है, जहाँ मानसिक सुधार और नैतिक प्रशिक्षण दरकार है, वहाँ कभी-कभी कुछ मनोवैज्ञानिक उपायों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक उपाय प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने भी प्रयोग किए हैं। सुन्नत में भी इसके इशारे मिलते हैं और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन के बाद आनेवाले प्रशिक्षकों ने भी इन उपायों से काम लिया है।
[सहाबा ने जो भी तरीक़े अपनाए वे अल्लाह के रसूल की शिक्षाओं के अनुरूप अपनाए, जबकि बादवालों ने ख़ुद अपनी बुद्धि से नए-नए रास्ते और तरीक़े निकाले। इसलिए बादवालों की सहाबा से तुलना दुरुस्त नहीं है———अनुवादक]
इन मनोवैज्ञानिक उपायों का उद्देश्य केवल यह है कि सत्यमार्ग पर चलनेवाले मुसाफ़िर को वासनाओं से बचने का अभ्यास कराया जाए, नैतिक बुराइयों को उसके नफ़्स और दिल से निकाला जाए और नैतिक पराकाष्ठा से उसके नफ़्स और दिल को विभूषित किया जाए। हुज़ूरी (अल्लाह के सामने होने) के एहसास का दर्जा इन तीनों प्रयासों की सफल पूर्ति से ही प्राप्त हो सकता है।
हुज़ूरी के एहसास का यह अभ्यास इंसान को इस बात की और अधिक मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता उपलब्ध करता है कि वासनाओं से कैसे बचा जा सकता है और अल्लाह तआला के सामने हाज़िरी के एहसास को कैसे पक्का और जगाए रखा जा सकता है। जब तक ईमान की परिपक्वता और आख़िरत की जवाबदेही के एहसास के साथ-साथ यह हुज़ूरी का आभास ताज़ा और जाग्रत नहीं रहेगा। उस समय तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा। मन की इच्छाएँ क़ाबू में नहीं आएँगी “और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने मन को (बुरी) इच्छाओं से रोके रखा, तो उसका ठिकाना जन्नत है।” (क़ुरआन, 79:40-41) यह कैफ़ियत जहाँ बुद्धि और ज़ेहन, सोच और समझ का सुधार चाहती है वहाँ दिल के सुधार की माँग भी करती है। फिर ईमान जहाँ एक बौद्धिक पहलू रखता है कि मेरा ज़ेहन और मेरी बुद्धि इसपर सन्तुष्ट हो जाएँ कि ये तथ्य मुझे मानने हैं, वहाँ इसका एक बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू दिल की हालत भी है। हार्दिक दृष्टि से मुझे इस अक़ीदे पर शान्ति और सन्तुष्टि भी प्राप्त होनी चाहिए। इस क़ल्बी ईमान में शिद्दत भी पैदा होती रहती है और मज़ीद शक्ति भी प्राप्त होती रहती है। क़ल्बी ईमान के लिए अल्लाह से प्रेम ज़रूरी है। अल्लाह से प्रेम की अपेक्षा अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम है और उनसे प्रेम की अपेक्षा यह है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का पूर्ण आज्ञापालन किया जाए। कुरआन में कहा गया है, “अगर तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो फिर मेरा अनुपारल करो।” (क़ुरआन, 3:31) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और अल्लाह से यह सम्बन्ध जब क़ायम होता है और यह मुहब्बत जब पैदा होती है तो इसका आइडियल और मापदंड यह है कि पूर्ण सन्तुलन के साथ पैदा हो। अगर सन्तुलन बरक़रार नहीं रह सका तो इसकी वजह या तो प्रशिक्षण की कमी है, या इंसान के स्वभाव की कमज़ोरी है। हर व्यक्ति का स्वभाव इतना परिपूर्ण और सन्तुलित नहीं होता कि वह इस सन्तुलन को बरक़रार रख सके। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का जो प्रशिक्षण किया वही प्रशिक्षण का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसी प्रशिक्षण का नतीजा और प्रतीक प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की यह शान थी कि दिन में वे शह-सवार होते थे, मैदाने-जंग में तलवार के जौहर दिखाते थे और रात के समय इबादत गुज़ार राहिब की तरह होते थे।
हज़रत अली-बिन-अबी तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बारे में किसी शाइर ने लिखा है, वह दिन के समय उनसे मिलने गया तो देखा कि वह आम सरकारी अधिकारियों की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक ख़लीफ़ा के अन्दाज़ में अपने कर्त्तव्य निभा रहे थे। उसको सिवाय उनकी सादगी और विनम्रता के कोई बात असाधारण महसूस नहीं हुई। इत्तिफ़ाक़ से उसको रात के समय उस मस्जिद में जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ जहाँ हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) इबादत किया करते थे। वहाँ उसको एक बिलकुल ही दूसरा मंज़र नज़र आया। उसको उसने एक शेअर में बयान किया है। जिसमें है कि दिन को वह बादशाहों की तरह होते हैं और रात को अल्लाह से फ़रियाद की कैफ़ियत होती है। अल्लाह का ज़िक्र उनकी ज़बान से जारी होता है।
इसका नतीजा यह निकलता है कि इंसान एक साथ इस कैफ़ियत का नमूना बन जाता है कि वह सबके साथ होते हुए भी सबसे अलग रहता है। एक तरफ़ अल्लाह की इबादत अंजाम दी जा रही हो, एक तरफ़ इंसान अल्लाह के सामने विनम्रता का रवैया रखता हो। आनन्द और धन एवं ख्याति के मामले में निस्पृहता और ज़ुह्द (संयम) का रवैया रखता हो, लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी तरफ़ वह उन तमाम कर्त्तव्यों का भी पाबन्द हो जो ज़ाहिरी ज़िन्दगी में उससे सम्बन्धित हैं, वह शरई कर्त्तव्य हों, या सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हों, सामुदायिक कर्त्तव्य हों, या उसकी दूसरी पदगत ज़िम्मेदारियाँ हों, वह इन सबमें भरपूर हिस्सा लेता हो। तसव्वुफ़ ज़िन्दगी में भरपूर हिस्सा लेने का नाम है, ज़िन्दगी से पलायन का नाम नहीं है। मुजाहिदीने-इस्लाम का इतिहास संकलित किया जाए तो जितने पहली पंक्ति के मुजाहिदीन हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) और हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से लेकर आज तक पैदा हुए हैं उनमें बहुत-से नाम ऐसे हैं जो एक साथ जिहाद, शहादत, तसव्वुफ़ और आध्यात्मिकता के मैदान में भी बहुत ऊँचे नाम हैं।
हमारे यहाँ उपमहाद्वीप में इस्लाम जिन व्यक्तियों की वजह से आया वे आम तौर से यही सूफ़िया थे, जिन्होंने तसव्वुफ़ के साथ-साथ इस्लाम का सन्देश दूसरों तक पहुँचाने का कर्त्तव्य भी पूरा किया। उनके साथ प्रशिक्षक सूफ़िया भी हर दौर में रहे हैं। जिन्होंने बड़ी संख्या में इंसानों का सुधार किया है। यह अक्सर वे सूफ़िया थे जो तसव्वुफ़ के बड़े-बड़े सिलसिलों के संस्थापक भी हैं।
जहाँ पवित्र क़ुरआन ने सकारात्मक रूप से नैतिक पराकाष्ठा की शिक्षा दी है, वहाँ नकारात्मक रूप से नैतिक बुराइयों से बचने का आदेश भी दिया है। चुनाँचे ‘हिर्स’ (लालच) से मना किया है। ‘हसद’ (ईर्ष्या) और ‘ग़ज़ब’ (क्रोध) से मना किया है, कंजूसी से मना किया है। घमंड से रोका है। ‘रिया’ (दिखावे) को बुरा क़रार दिया है। ये तमाम ख़राबियाँ दिल की ख़राबियाँ हैं। जैसे ज़ाहिरी कर्मों से सम्बन्धित निषिद्ध कार्य हैं उसी तरह दिली कैफ़ियत के लिए भी कुछ निषिद्ध स्थितियाँ हैं। एक आम इंसान के लिए ज़ाहिरी तौर से अन्दाज़ा करना आम तौर पर बड़ा कठिन होता है कि मेरे दिल में ईर्ष्या की भावना कितनी है या घमंड कितना है। घमंड का इज़हार अगर कर्मों में हो तो किसी हद तक उसका अन्दाज़ा हो जाता है, लेकिन अगर कर्मों या ज़बान से इसका इज़हार न हो तो कभी-कभी इसका अन्दाज़ा नहीं होता। और कर्म से इज़हार भी कभी-कभी ऐसे सूक्ष्म ढंग से होता है कि बड़े-बड़े विशेषज्ञों के सिवा किसी को अन्दाज़ा नहीं होता कि यह घमंड है।
जिन लोगों ने इन विषयों पर लिखा है उदाहरणार्थ इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने और हज़रत मुजद्दिद साहब और दूसरे बुज़ुर्गों ने। उनकी बहसों में इतने बारीक नुक्ते महसूस होते हैं जिन तक आम ज्ञानी लोगों की नज़र नहीं जाती। हज़रत मुजद्दिद साहब ने एक जगह लिखा है कि कभी-कभी ‘तवाज़ो’ (विनम्रता) ‘किब्र’ (घमंड) की चादर ओढ़कर सामने आती है। कभी-कभी ‘किब्र’ (घमंड) ‘तवाज़ो’ (विनम्रता) का चोला ओढ़कर सामने आता है। अन्दर से ‘किब्र’ होता है, लेकिन इसका इज़हार ‘तवाज़ो’ के अन्दाज़ से होता है। यह इंसान की एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक कमज़ोरी है। इस तरह की ख़राबियाँ अनगिनत हैं जिनको दूर करने के लिए फ़ुक़हा-ए-नफ़्स की ज़रूरत पड़ती है। और फ़िक़्हुन-नफ़्स ही वह मैदान है जिसको ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की शब्दावली से याद किया गया है।
पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह ज़िक्र की शिक्षा दी है। “अल्लाह को बहुत अधिक याद करो”, “तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा।” सवाल यह है कि ऐसा करने से क्या मुराद है? यहाँ अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है? इसके बारे में हमारे ज़माने के कुछ लोगों को पारम्परिक ‘ज़िक्र’ की धारणा पर सन्तोष नहीं है। उनका कहना है कि अल्लाह को याद करने से मुराद यह है कि अल्लाह की शरीअत और आदेशों को याद रखा जाए। निश्चय ही यह याद भी ‘ज़िक्र’ के अर्थ में शामिल है, लेकिन पवित्र क़ुरआन की बहुत-से आयतों से स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि मात्र आदेशों को याद रखना ज़िक्र के लिए काफ़ी नहीं है। आदेशों की याद और ख़याल ‘ज़िक्र’ का अनिवार्य परिणाम और अपेक्षा होनी चाहिए। पवित्र क़ुरआन ने ईमानवालों के बारे में कहा है कि ये वे लोग हैं जो दिन में और रात को लेटे हों या बैठे हों, सो रहे हों या जाग रहे हों, बिस्तर पर हों, या खड़े हों, ये अल्लाह को याद करते हैं। यहाँ अल्लाह को याद करने से मुराद मात्र उसके आदेशों को याद रखना नहीं, बल्कि यहाँ स्पष्ट रूप से ज़बान से ‘ज़िक्र’ करना मुराद है कि ज़बान से हर समय अल्लाह तआला को याद करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विभिन्न अवसरों के लिए विभिन्न ‘ज़िक्र’ की शिक्षा भी दी है। हदीसों की किताबों में बहुत अधिक और निरन्तरता के साथ यह निर्देश मिलते हैं कि सुबह सोकर उठो तो यह दुआ पढ़ो, रात को बिस्तर पर जाओ तो यह दुआ पढ़ो। अमुक गतिविधि हो तो यह दुआ पढ़ो। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि ज़िक्र से मुराद बहुत-सी आयतों में केवल ज़बान से ‘ज़िक्र’ करना है। ज़बान से अल्लाह को याद करने के जो विभिन्न फ़ार्मूले हदीसों में बयान हुए उनपर अमल करना पवित्र क़ुरआन के आदेशों की एक अनिवार्य अपेक्षा है। ‘ज़िक्र’ के इन आदेशों पर कार्यान्वयन को अमल (कर्म) से पलायन क़रार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसी अमल की तैयारी के लिए, उसी ज़िम्मेदारी का एहसास बरक़रार रखने के लिए ये ‘ज़िक्र’ मुसलमानों को सिखाए गए हैं। यह भी बताया गया कि ‘ज़िक्र’ ज़बान से भी करो, दिल में भी करो, बुलन्द आवाज़ से भी करो, और आहिस्ता आवाज़ से भी करो। कभी-कभी बुलन्द आवाज़ से ‘ज़िक्र’ लाभदायक होता है। कभी-कभी आहिस्ता आवाज़ से ‘ज़िक्र’ लाभदायक होता है। इसका सम्बन्ध सम्बन्धित व्यक्ति के निजी स्वभाव से होता है और उनका इस अवसर की दृष्टि से प्रशिक्षण ज़रूरी भी है।
प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न अन्दाज़ से ‘ज़िक्र’ करते थे। दूसरे अनेक मामलों के अलावा इस मामले में भी प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में विभिन्न रुचियों के लोग मौजूद थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक बार प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की रात की इबादत का जायज़ा लेने के लिए गए। देखा कि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) बहुत धीमी आवाज़ से तिलावत या ज़िक्र कर रहे थे। हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को देखा कि बहुत बुलन्द आवाज़ से ‘ज़िक्र’ या तिलावत कर रहे थे। अगले दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पूछा कि तुम ज़िक्र धीमी आवाज़ से क्यों-कर रहे थे? सिद्दीक़ अकबर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फ़रमाया जिसको सुना रहा था वह दिलों के भेद भी जानता है। अत: किसी बुलन्द आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत अमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से पूछा कि तुम बुलन्द आवाज़ में ज़िक्र क्यों कर रहे थे? कहने लगे कि मैं ज़िक्र के साथ-साथ सोए लोगों को जगाना चाहता था, ग़ाफ़िलों को सचेत भी करना चाहता था और दुश्मनों के दिलों को जलाना भी चाहता था।
अब आप देखें कि यहाँ अल्लाह का ‘ज़िक्र’ किया जा रहा है, लेकिन ‘ज़िक्र’ के साथ-साथ दूसरे उद्देश्य और प्रेरक भी मौजूद हैं। इससे पता चला कि रुचियाँ विभिन्न इंसानों की विभिन्न हो सकती हैं। जब दो बड़े सहाबा की दो विभिन्न रुचियाँ हो सकती हैं तो शेष प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी बहुत-सी रुचियाँ सम्भव हैं। अब जब ये सहाबा अपने-अपने शिष्यों का दीनी (धार्मिक) सुधार और प्रशिक्षण करेंगे तो उनके शागिर्दों की रुचियाँ भी भिन्न होंगी। और जो शिष्यों की रुचि बनेगी तो वह फिर आगे चलकर शिष्यों के पूरे सिलसिले में नुमायाँ होगी। इसलिए जिन लोगों ने ज़िक्र के इस आदेश को या ज़िक्र की इस शिक्षा को प्रशिक्षण का एक हिस्सा बनाया, उनमें विभिन्न अन्दाज़ या शैलियाँ हमें मिलती हैं। ख़ुद हमारे दौर में दक्षिण-एशिया में, उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप से बाहर विभिन्न मज़हबी आन्दोलनों के पेशवाओं ने, दीनी प्रशिक्षण करनेवालों और मुस्लिम समुदाय के सुधार का काम करनेवालों ने ज़िक्र को किसी-न-किसी हैसियत में अपने प्रशिक्षण का एक अंग बनाया। अल-इख़वानुल-मुस्लिमून के संस्थापक हसनुल-बन्ना शहीद स्वयं एक तब्लीग़ी और आध्यात्मिक सिलसिले से जुड़े थे। उन्होंने दुआओं का एक संग्रह संकलित किया। वह संग्रह एक ज़माने में बहुत लोकप्रिय था और अल-इख़वानुल-मुस्लिमून से जुड़े लोग इस संग्रह को प्रयोग किया करते थे। जब सऊदियों की हुकूमत शुरू-शुरू में क़ायम हुई तो सुलतान अब्दुल-अज़ीज़ ने दुआओं का एक संग्रह संकलित किया था जो एक लम्बे अर्से तक सऊदियों में और ऑले-सऊद में लोकप्रिय रहा। ये दुआएँ वे थीं जो पवित्र क़ुरआन या हदीसों में आई हैं। लेकिन उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार चुनी हुई दुआओं का एक संग्रह संकलित किया और उनके माननेवालों ने इसको अपनाया।
आम तौर से कहा जाता है कि सूफ़ी लोग अपने ज़माने के ‘अहदी’ हुआ करते थे। उर्दू में अहदी का शब्द एक बेकार, सख़्त, नालायक़ और कमज़ोर आदमी के लिए प्रयोग होने लगा है। सूफ़िया के बारे में आम तौर पर तसव्वुर यह है कि जितने सूफ़ी लोग होते हैं वे ‘अहदी’ होते हैं। और अहदी बनने में या उनको काम चोरी और अमल से भागने में ‘तवक्कुल’ (अल्लाह पर भरोसा) की ग़लत धारणा ने और भी सुविधा दी है। बड़े सूफ़ी लोगों के यहाँ ‘तवक्कुल’ की जो धारणा है वह ठीक वही है जो पवित्र क़ुरआन और हदीस में बयान हुई है। ‘तवक्कुल’ का शाब्दिक अर्थ तो है ‘भरोसे का रवैया अपनाना’, लेकिन शब्दावली में ‘तवक्कुल’ से मुराद यह है कि साधनों को अपनाने के बाद साधनों के परिणाम को अल्लाह तआला पर छोड़ देना और फिर जो परिणाम सामने आए उसको अल्लाह का फ़ैसला समझकर उसपर राज़ी रहना। ‘तवक्कुल’ का यह अर्थ उस प्रसिद्ध हदीस पर आधारित है जिसमें बताया गया है अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से मिलने के लिए एक नौ-मुस्लिम बद्दू सहाबी मदीना मुनव्वरा आए और बहुत भावना से नबी की सेवा में हाज़िर हुए। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा कि “जानवर कहाँ छोड़ा?” यानी जिस ऊँट पर सवार होकर आए थे, वह कहाँ है? उन्होंने बताया कि “मैंने बाहर छोड़ दिया है।” फ़रमाया, “क्यों?” उन्होंने कहा, “अल्लाह पर तवक्कुल किया है। इसलिए उसको छोड़ आया हूँ।” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “नहीं, बाहर जाओ! पहले उसे बाँध दो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो।” यानी जानवर की सुरक्षा का जो कम-से-कम तरीक़ा या साधन है उसको अपनाओ। उस साधन को अपनाने के बाद फिर परिणाम को अल्लाह पर छोड़ दो।
इससे इस्लाम के बड़े विद्वानों ने यह नतीजा निकाला कि किसी चीज़ के अनिवार्य और प्रचलित साधनों का अपनाना ‘तवक्कुल’ के विरुद्ध नहीं है। अत: साधनों को अपनाना चाहिए, लेकिन अपनाने के बाद परिणाम को अल्लाह की मशीयत (नियति) के सिपुर्द कर देना चाहिए और जो परिणाम सामने आए उसको अल्लाह का फ़ैसला समझकर उसपर राज़ी हो जाना चाहिए।
साधनों को अपनाने के तीन दर्जे हैं, एक दर्जा तो वह है जो अभीष्ट है। उसके लिए हदीस में कहा गया, “साधनों को अपनाने में और किसी भौतिक चीज़ की प्राप्ति में दरमयाने रास्ते को अपनाओ।” साधनों ही को सब कुछ समझकर केवल साधनों के पीछे मत पड़ो।
‘तवक्कुल’ का यह अर्थ कि तमाम साधन छोड़ दिए जाएँ और कोई साधन सिरे से अपनाया न जाए और फिर यह उम्मीद बाँध ली जाए कि अल्लाह तआला की तरफ़ से ख़ुद-ब-ख़ुद परिणाम निकल आएँगे, यह शरीअत की शिक्षा और स्वभाव के ख़िलाफ़ है। ऐसा ‘तवक्कुल’ अपनाना अल्लाह तआला की मर्ज़ी नहीं है।
यह और इस तरह की शिक्षा उन नैतिक क़ल्बी (हार्दिक) और आध्यात्मिक मामलों के बारे में है जिनके बारे में पवित्र क़ुरआन ने स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिए हैं। कुछ नैतिक पराकाष्ठाएँ हैं, या दिल के कार्य हैं जिनको प्राप्त करना चाहिए। कुछ दिल की कैफ़ियतें हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए।
अनुभव से यह भी पता चला कि कुछ ज़ाहिरी कर्मों का प्रभाव इंसान के आन्तरिक और गुप्त कर्मों पर भी पड़ता है। इसलिए जब प्रशिक्षण की बात आएगी और कोई शैख़ या कोई प्रशिक्षक किसी शिष्य का प्रशिक्षण करेगा तो वह यह भी देखेगा कि इस के ज़ाहिरी कर्म और तौर-तरीक़ों में किन-किन सुधारों की ज़रूरत है। अगर कोई प्रशिक्षण करनेवाला प्रशिक्षण की अपेक्षा यह समझे कि किसी जायज़ काम के करने पर सज़ाएँ लागू की जाएँ, तो यह अस्थायी हदबन्दी या परहेज़ प्रशिक्षण के विरुद्ध नहीं है और इससे शरीअत के आदेशों का उल्लंघन नहीं होता।
मिसाल के तौर पर एक आम अवलोकन है कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा खाए तो तबीअत सुस्त हो जाती है, और जब तबीअत सुस्त हो जाए तो इबादतों में वह सन्तोष, मिठास और क़ुरआन पाक की तिलावत (पाठ) में वह आनन्द महसूस नहीं होता जो होना चाहिए। रात को बहुत ज़्यादा खाकर सो जाने से तहज्जुद की नमाज़ के लिए जागना और सुकून से इबादत करना मुश्किल हो जाता है। इबादतों में सुस्ती पैदा हो जाती है। इसलिए अगर कोई प्रशिक्षक और शैख़ अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था का एक अंग यह भी क़रार दे कि जब तक किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण हो रहा है उस समय तक उसके खान-पान को सीमित कर दिया जाए, कुछ ख़ास-ख़ास समयों में खाने की मनाही कर दी जाए, या कुछ चीज़ों की खाने की मनाही कर दी जाए तो यह प्रशिक्षण का एक अंग है जो कभी-कभी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण का एक अंग क़रार दिया जाता है। इसी तरह ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हँसना ग़फ़लत (भुलावा) पैदा करता है। इसलिए ज़ाहिरी कर्मों के इन परिणामों की वजह से कुछ बुज़ुर्गों ने इन चीज़ों को कम या संगठित करना चाहा। चुनाँचे कुछ सूफ़ियों के यहाँ कम खाने, कम बोलने, कम सोने और लोगों से कम मिलने-जुलने पर बहुत ज़ोर दिया गया कि कम खाओ, कम बोलो, कम सोओ, और लोगों से कम मिलो। यह भी आम अनुभव और अवलोकन की बात है कि ज़्यादा मेल-जोल से ज़िम्मेदारियों और कर्त्तव्यों को निभाने में लापरवाही पैदा होती है। ग़ैर-ज़रूरी मेल-जोल में वृद्धि हो जाए तो इंसान बहुत-से गम्भीर मामलों पर ध्यान नहीं दे पाता। यह भी आम अनुभव और अवलोकन की बात है। इसलिए प्रशिक्षण के मामले में जब सूफ़ी लोगों ने और प्रशिक्षण देनेवाले बुज़ुर्गों ने इन शैलियों की निशानदेही करनी चाही जिन शैलियों से मदद लेकर लोगों का प्रशिक्षण किया जा सके तो बहुत-से साधन उन्होंने ऐसे भी अपनाए जिनकी प्रत्यक्ष रूप से माँग क़ुरआन और सुन्नत ने नहीं की थी। यानी वे कर्म अपने-आपमें शरई तौर पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं थे, लेकिन समय के निहितार्थ के तहत अनिवार्य थे। उस सामयिक निहितार्थ में संशोधन भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है। बाद में आनेवाले पहले आनेवालों से भी मतभेद कर सकते हैं और हालात और ज़माने को देखते हुए उनमें परिवर्तन भी हो सकता है।
इन तमाम प्रयासों का मौलिक उद्देश्य यही था कि कर्म में निष्ठा पैदा हो और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास जाग्रत हो, ताकि उस हदीस पर अमल हो सके, जिसमें कहा गया है कि “तुममें से कोई शख़्स उस वक़्त तक ईमानवाला नहीं हो सकता जब तक उसकी इच्छाएँ उस (शरीअत) के अधीन न हो जाएँ जिसे मैं लेकर आया हूँ।”
तसव्वुफ़ के बारे में विशेष रूप से और दूसरी बहुत-सी दीनी गतिविधियों के बारे में आम तौर पर एक बात और भी उल्लेखनीय है। इंसानों की विशेषता यह है कि जब कोई सोच, कोई आह्वान, कोई मिशन या कोई सन्देश किसी विशेष वातावरण में अपनी जगह बनाता है तो वहाँ उसका एक निर्धारित और व्यावहारिक रूप जन्म लेता है, जिसके परिणामस्वरूप उस नज़रिये या दावत को institutionalize किया जाता है। इस institutionalization के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ नुक़सानात भी होते हैं। लाभ तो यह है कि उस सन्देश के यों संस्था बन जाने से कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है। यह सुचारू रूप जब बहुत मुद्दत तक जारी रहे तो इससे एक तरह की समरूपता पैदा हो जाती है। कार्य में समरूपता और निरन्तरता पैदा हो जाती है। इस समरूपता और निरन्तरता का परिणाम यह निकलता है कि लोग उससे ख़ूब अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। आगे चलकर बाद में आनेवाले यह अन्तर नहीं कर पाते कि इस सन्देश का मूल उद्देश्य क्या था और ये institution किस उद्देश्य की ख़ातिर बनाया गया था। उनमें से बहुत-से जोशीले अन्धानुकरण करनेवाले और कम समझ अनुयायी यह अन्दाज़ा नहीं करते, या नहीं कर सकते कि सन्देश में मूल उद्देश्य क्या था, अभीष्ट भाग कौन-सा था, और इस सारे काम में साधन की हैसियत किस पहलू को प्राप्त थी। रणनीति के तहत कौन-कौन सी चीज़ें अपनाई गई थीं। यों उद्देश्यों और संसाधनों में अन्तर नज़रों से ओझल हो जाता है।
यह बात कि संसाधनों और उद्देश्यों में अन्तर न किया जा सके, यह बाद में आनेवालों में अधिकांश के साथ होता है और हर दौर में हुआ है। फ़िक़्ह में भी हुआ है, तसव्वुफ़ में भी हुआ है, कलाम में भी हुआ है। और तफ़सीर और हदीस के मामले में भी हुआ है। नवीनीकरण और पुनरुत्थान के आन्दोलनों में भी हुआ है, दीनी तहरीकों में भी हुआ है और दूसरी संस्थाओं में भी हुआ है। उदाहरणार्थ पढ़ने-पढ़ाने की संस्थाएँ स्थापित की गईं, उद्देश्य क्या था? केवल दीनी प्रशिक्षण को उपलब्ध करना और दीनी उलूम (धार्मिक ज्ञान) का प्रचार-प्रसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ संसाधन प्रयोग किए गए, कुछ स्थितियों में इन संसाधनों ने अस्ल उद्देश्यों की हैसियत अपना ली। यों वे गौण मामले जो वस्तुतः संसाधन थे, बाद में आनेवाले लोगों की नज़र में मूल उद्देश्य बन गए और यों इस कम समझ और जोशीले अन्धानुकरण के परिणामस्वरूप जो मूल उद्देश्य थे वे पीछे चले गए।
यह त्रासदी केवल तसव्वुफ़ के साथ नहीं हुई, यह सबके साथ हुआ है। एक चरण आता है कि नाम रह जाता है और वास्तविकता गुम हो जाती है। हमारा दौर तो एक हज़ार साल बाद का है। शैख़ अली हजवेरी ने एक बुज़ुर्ग का क़ौल (कथन) नक़्ल किया है वह अपनी किताब ‘कशफ़ुल-महजूब’ में कहते हैं कि आजकल तसव्वुफ़ एक नाम है बिना वास्तविकता के। यानी पाँचवीं शताब्दी हिजरी में ही उन्होंने यह महसूस किया कि पिछले ज़माने में यह एक वास्तविकता थी बिना नाम के, गोया पहले ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ की एक वास्तविकता थी, बाद में इस वास्तविकता को एक नाम मिला, नाम के बाद इसको प्राप्त करने का एक तरीक़ा सामने आया। इस तरीक़े पर अमल करने के लिए कुछ लोग निर्धारित हो गए। जब व्यक्ति निर्धारित हुए तो उनकी सुविधा की ख़ातिर कुछ संस्थाएँ अस्तित्व में आईं। जब संस्थाएँ अस्तित्व में आईं तो संस्थाओं को चलाने के लिए संसाधन सामने आए। अब संसाधन ही लोगों का उद्देश्य बन गए और संसाधनों के अलावा बाक़ी चीज़ें उनकी नज़रों से ओझल हो गईं।
यह बात कि मानव मन को अल्लाह की इबादत के लिए तैयार किया जाए, इस तैयारी में सूफ़ियों के दरकार कमालात और आध्यात्मिक विकासों को प्राप्त करने की कोशिश की जाए, जिन नैतिक पराकाष्ठा की शरीअत ने शिक्षा दी है वह न केवल सबको प्राप्त हो जाए, बल्कि ईमानवालों की नस-नस का हिस्सा बन जाएँ और जिन बुराइयों से बचने का शरीअत ने आदेश दिया है वे दिल से पूरे तौर पर निकल जाएँ। यही वे उद्देश्य हैं, जो तसव्वुफ़ से लोगों के सामने थे। विद्वानों ने अपने-अपने ज़माने में ये परिभाषाएँ और शब्दावलियाँ जनसाधारण को समझाने की ख़ातिर इन तथ्यों और शिक्षाओं को बयान करने के लिए तैयार की थीं जो एक-एककर नज़र-अन्दाज़ होती चली गईं। लेकिन यह बात पहले दिन से बड़े विद्वानों के सामने थी और हमेशा सामने रही कि शिक्षा और प्रशिक्षण की यह सारी व्यवस्था शरीअत ही का एक हिस्सा है। शरीअत ही के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है और शरीअत के शेष दो पहलुओं को नज़र-अन्दाज़ करके अगर कोई और रास्ता अपनाया जाएगा तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।
इमाम मालिक (रह॰) का एक वाक्य प्रसिद्ध है। इमाम मालिक (रह॰) की अपनी किसी किताब में तो नहीं देखा, लेकिन उनसे सम्बद्ध है। वाक्य बड़ा ज़बरदस्त है। अगर उनका नहीं भी है तो जिसका भी है उसने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि “जिसने तसव्वुफ़ के रास्ते को अपनाया और फ़िक़्ह के आदेशों को नहीं अपनाया यानी शरीअत के दूसरे दो हिस्सों पर अमल नहीं किया, उसने गोया ज़िंदीक़ियत (नास्तिकता) का रास्ता अपनाया। उसकी मंज़िल आख़िरकार ज़िंदीक़ियत है और वह ज़िंदीक़ होकर रहेगा। जो व्यक्ति सिर्फ़ शरीअत के ज़ाहिरी पहलुओं पर ध्यान देगा और अन्दर से आन्तरिक पहलू को ध्यान का हक़दार नहीं समझेगा वह फ़ासिक़ (उल्लंघनकारी) हो जाएगा।” वास्तविकता यह है कि जब शरीअत के आदेशों की पैरवी अन्दर से न हो, मात्र ज़ाहिरदारी से की जा रही हो तो इंसान ज़ाहिरदारी के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ कर लेता है। उसके अन्दर रूह बाक़ी नहीं रहती। “और जिसने इन दोनों को एक साथ अपनाया वह वास्तविकता को पा गया।” जुनैद बग़्दादी सूफ़ियों के इमाम और तीसरी शताब्दी हिजरी के पहली पंक्ति के प्रशिक्षक और ‘तज़किया’ वालों में से हैं। उनका यह वाक्य इमाम ग़ज़ाली, शैख़ अली हजवेरी और कई लोगों ने अपनी-अपनी किताबों में उद्धृत किया है, “हर वह तरीक़ा जो शरीअत में अस्वीकार्य हो वह ज़ंदक़ा है।”
अत: फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ दोनों शरीअत ही के दो पहलू हैं। दोनों एक ही वास्तविकता के दो रुख़ हैं। अगर एक फ़िक़्हुन-नफ़्स है, तो दूसरा फ़िक़्हुल-अमल है। अगर एक फ़िक़्हुल-जवारेह है तो दूसरा फ़िक़्हुल-क़ल्ब है। तसव्वुफ़ न हो तो फ़िक़्ह की वास्तविकता पर कार्यान्वयन मुश्किल है। और फ़िक़्ह न हो तो तसव्वुफ़ पर कार्यान्वयन मुश्किल है। और फ़िक़्ह न हो तो तसव्वुफ़ पर कार्यान्वयन का दावा मात्र ज़ंदक़ा है। और इन दोनों के बिना पूरे ईमान का पूरा होना बड़ा मुश्किल है। ईमान की मिठास मेरे अन्दर है या नहीं है, यह मात्र एक आभासी और आन्तरिक चीज़ है। आप उसे न किसी तराज़ू से तौल सकते हैं, न किसी ज़ाहिरी और भौतिक पैमाने से नाप सकते हैं। न कोई ऐसा यंत्र पाया जाता है जो ईमान की गर्मी को महसूस करके नाप सके। यह तो एक साहबे-ज़ौक़ इंसान ख़ुद महसूस कर सकता है कि उसके दिल में ईमान की मिठास है कि नहीं है। इसलिए पहले के विद्वानों के यहाँ इन चीज़ों को बयान करने की प्रवृत्ति नहीं थी। वे यह समझते थे कि किसी आध्यात्मिक कैफ़ियत का पाया जाना एक विशुद्ध आन्तरिक चीज़ है और मेरे और अल्लाह के दरमियान एक राज़ है, इसको दूसरों से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यह शिक्षा संकलित होनी शुरू हुई, इसपर किताबें लिखी जाने लगीं तो उन आन्तरिक अनुभवों के विवरण भी लिखे जाने लगे। इन अनुभवों को बयान करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि वास्तविक अनुभव को वहमी और अवास्तविक अनुभव से अलग किया जाए, और लोगों को यह बताया जाए कि उनके ‘वारदात’ (अनुभवों) में क्या चीज़ सही है और क्या ग़लत। बहरहाल जब इन नाज़ुक मामलों को बयान करने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसके लिए मजाज़ और इस्तिआरा (अलंकार) का रंग अपनाना पड़ा। इन अनुभवों को बयान करने में शब्द कम पड़ने लगे, मजबूरन ऐसे बहुत-से शब्द प्रयोग किए गए जो दरअस्ल मजाज़ और इस्तिआरे का रंग रखते हैं।
अभी हलावत का मैंने ज़िक्र किया है। सम्बन्धित हदीसों में ‘हलावत’ (मिठास) का शब्द एक मजाज़ी और इस्तिआरे (अलंकार) के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यही हाल शेष शब्दावलियों का भी है। उनमें से अधिकांश शब्दावलियों में तशबीह (उपमा), मजाज़ और इस्तिआरे से काम लिया गया, इसलिए कि तसव्वुफ़ के अधिकांश तथ्यों का सम्बन्ध आन्तरिक अनुभव और आभासी मामलों से है। इसलिए सूफ़ी लोगों की बहुत-सी शब्दावलियों की व्याख्या उनके विशुद्ध ज़ाहिरी और शब्दकोशीय अर्थों के अनुसार करना दुरुस्त नहीं। जिस तरह ‘हलावत’ की शाब्दिक व्याख्या नहीं हो सकती, इसी तरह शेष शब्दावलियों की भी नहीं हो सकती। दुनिया के शेष तमाम ज्ञान-विज्ञान में यह बात निस्संकोच स्वीकार की जाती है कि शब्दावली की व्याख्या का अधिकार शब्दावली देनेवाले ही को प्राप्त होता है। यह नहीं हो सकता कि क़ानूनविदों की शब्दावली की व्याख्या करें मिल्ट्री के लोग, और मिल्ट्री शब्दावलियों की व्याख्या करें फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक), और दर्शन की शब्दावलियों की व्याख्या करें मिसाल के तौर पर व्यापार विशेषज्ञ। अगर ऐसा होने लगे तो तमाम शब्दावलियों का अर्थ ग़लत क़रार पा जाएगा और उन तथ्यों की सटीक व्याख्या नहीं हो सकेगी जिन तथ्यों की वे शब्दावलियाँ प्रतिनिधि या प्रवक्ता हैं।
तसव्वुफ़ की शब्दावलियाँ समय के साथ-साथ फैलती गईं और बढ़ती गईं। इन शब्दावलियों में छठी, सातवीं, बल्कि आठवीं शताब्दी हिजरी के बाद एक नया रंग पैदा हुआ। अभी तक यानी छठी सदी हिजरी तक तसव्वुफ़ पर लिखी हुई अधिकांश लेखन सामग्री उन विद्वानों की संकलित की हुई थी जो आलिम होने के साथ फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) भी थे, मुतकल्लिम भी थे, मुहद्दिस और मुफ़स्सिर (क़ुरआन के टीकाकार) भी थे। छठी शताब्दी हिजरी के मध्य से पहले की तसव्वुफ़ की किताबों में से अधिकांश के लेखक उनमें से अधिकतर मैदानों के माहिर थे। उदाहरणार्थ इमाम अबुल-क़ासिम क़ुशैरी, अबू-नस्र सिराज, कलाबाज़ी, ग़ज़ाली (रह॰) और दूसरे लोग। सातवीं शताब्दी हिजरी के बाद से इस मैदान में अदीब (साहित्याकर) भी दाख़िल हो गए, शाइर भी मैदान में आ गए। बहुत-से शाइरों और अदीबों ने तसव्वुफ़ की बातों को अपनी-अपनी किताबों में बयान करना शुरू किया। इन शाइरों और अदीबों में कुछ तो उलमा (इस्लामी विद्वान) थे, उदाहरणार्थ मौलाना रूमी, और मौलाना जामी। कुछ ऐसे लोग थे जो उलमा नहीं थे या उस दर्जे के उलमा नहीं थे, लेकिन यह शब्दावलियाँ सबने अपनाईं और इन शब्दावलियाँ में और बढ़ोतरी की। शाइरों में बहुत-से ऐसे भी थे जो तसव्वुफ़ की बातों से मात्र शाइराना दिलचस्पी रखते थे और अस्ल हक़ीक़तों, उसकी बुलन्दियों से उनका निजी व्यावहारिक या अनुभव सम्बन्धी वास्ता न था।
जिस ज़माने में सूफ़ियाना बातों को शाइरी में कहनेवाले शाइर सामने आए, यह वह ज़माना था जब मुसलमानों का राजनैतिक और सामाजिक पतन बहुत निचली हदों को छू रहा था। बग़दाद का पतन हो चुका था। तातारियों ने पूरे मुस्लिम जगत् को बर्बाद कर दिया था, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान शहीद हो चुके थे और मुसलमानों का कोई राजनैतिक स्थान या गरिमा दुनिया में नहीं रही थी और हर ओर निराशा फैल रही थी। इस निराशा की स्थिति में कुछ सूफ़ी लोगों ने मुसलमानों को उम्मीद का सन्देश देना चाहा। जिनमें सबसे बड़ा नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है। उन्होंने इतने ज़ोर-शोर से ‘रजाइयत’ (आशावाद) का यह नग़मा बुलन्द किया और लोगों को ऊँची आवाज़ से यह बात याद दिलाई कि इस्लाम का उद्देश्य किसी भौतिक हित की प्राप्ति नहीं है, या राज्य और सल्तनत की स्थापना मूल उद्देश्य नहीं है, यह एक दूसरे दर्जे की चीज़ है। अस्ल चीज़ चरित्र और व्यक्तित्व का गठन और निर्माण है। आध्यात्मिकता का गठन और निर्माण है।
उस ज़माने में तसव्वुफ़ के समर्थकों में मौलाना रूमी की ‘मसनवी’ बहतु लोकप्रिय हुई। ‘मसनवी’ की लोकप्रियता से प्रभावित होकर, या किसी और वजह से, या उस ज़माने के हालात और रंग को देखकर, बहुत-से ऐसे शाइर भी इस मैदान में आ गए जिनका अपना मक़ाम और मर्तबा वास्तविक आध्यात्मिकता के मैदान में सन्दिग्ध क़रार दिया जा सकता है। उनमें से कुछ का स्थान इस मैदान में इतना ऊँचा नहीं था जितना मौलाना रूमी और उनके दर्जे के दूसरे लोगों का था।
[यह स्थान कैसे तय होगा, इसका पैमाना क्या है, तसव्वुफ़ के समर्थक इसे आज तक स्पष्ट रूप से बता नहीं सके।———अनुवादक]
ऐसे आम शाइरों ने भी शेरो-शाइरी के साधन को अपनाया और इस शेरो-शाइरी के ज़रिये को अपनाने की वजह से ये शब्द और धारणाएँ पूरे मुस्लिम जगत् में लोकप्रिय हो गईं। ये दूसरे लोग जो बाद में सामने आए, उनमें हाफ़िज़ शीराज़ी की मिसाल मैं नुमायाँ तौर पर देना चाहता हूँ। उनके शाइराना कमालात ने जहाँ उनके कलाम को मुस्लिम जगत् के चप्पे-चप्पे में तुर्की से बंगाल तक और तुर्किस्तान औप तातारिस्तान से दक्कन (दक्षिण भारत) तक आम किया, वहाँ सूफ़ियाना बातों और सूफ़ियाना शब्दावलियों को भी घर-घर आम कर दिया। हाफ़िज़ शीराज़ी वाक़ई साहबे-हाल सूफ़ी थे कि नहीं थे, यह अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ लोग उनको बहुत बड़ा सूफ़ी समझते हैं और उनके अशआर की इसी तरह व्याख्या करते हैं, जिस तरह बड़े सूफ़ियों के कलाम की जाती है। कुछ दूसरे लोग उन्हें इसी तरह का एक आम शाइर समझते हैं जैसे और शाइर होते हैं और गुलो-बुलबुल की शाइरी करने से ज़्यादा उनकी कोई ग़रज़ नहीं होती। कुछ आलोचक और विद्वान लोगों के ख़याल में हाफ़िज़ के कलाम के सकारात्मक पहलुओं के सकारात्मक और लाभकारी प्रभाव भी हुए। अल्लामा इक़बाल उनके प्रभाव को बहुत नकारात्मक क़रार देते हैं।
हाफ़िज़ और हाफ़िज़ जैसे बहुत-से शाइरों की वजह से ऐसी आन्तरिक धारणाएँ भी मुसलमानों में फैल गईं जो दरअस्ल बड़े सूफ़ी लोगों की धारणाएँ नहीं थीं। या सूफ़ी लोगों के यहाँ उनपर वह ज़ोर नहीं दिया जाता था या वह क्रम और प्राथमिकता नहीं थी जो हाफ़िज़ के कलाम से सामने आई। फिर जब हाफ़िज़ और दूसरे शाइरों ने सूफ़ियाना शब्दावलियाँ प्रयोग करनी शुरू कीं तो उनके कलाम के द्वारा ऐसी शब्दावलियाँ भी सामने आने लगीं जो विशुद्ध वासनात्मक उद्देश्यों और भौतिकवादी मामलों के लिए प्रयुक्त होती हैं। चुनाँचे ‘क़ामत’ और ‘ज़ुल्फ़’, ‘ख़त’ और ‘अब्रू’ और ‘शराब’ और ‘नशा’ और इस तरह की सारी शब्दावलियाँ आम हो गईं जिनके बारे में यह निर्धारण करना कठिन है कि शाइर ने इन शब्दावलियों को किस अर्थ में प्रयुक्त किया है। इन ‘रुमूज़’ (बारीकियों) के बारे में यक़ीन से यह कहना बहुत कठिन बात है कि इन ‘रुमूज़’ का उद्देश्य वाक़ई आध्यात्मिक रहस्य हैं या उनके द्वारा जाने-अनजाने ‘बातिनियत’ (रहस्यवाद) और ‘इबाहियत’ (स्वच्छन्दता) के लिए मार्ग सुगम किया जा रहा है।
यहाँ तक कि हमारे मिर्ज़ा ग़ालिब ने भी सूफ़ियाना बातों और सूफ़ियाना शब्दावलियों को अपने कलाम में बहुत अधिक प्रयोग किया। कुछ लोगों ने मिर्ज़ा ग़ालिब के कलाम की व्याख्या इस तरह लिखी है कि उसमें और इमाम ग़ज़ाली की ‘एहयाउल-उलूम’ या मौलाना रूम की ‘मसनवी’ में कोई अन्तर बाक़ी नहीं रहता, लेकिन मिर्ज़ा ग़ालिब का जो रवैया और जीवन-प्रणाली थी वह सबको मालूम है। तसव़्वुफ और शरीअत से उनके सम्बन्ध की क्या कैफ़ियत थी यह भी कोई ढकी-छिपी बात नहीं है। चूँकि वे हमसे क़रीबी ज़माने के हैं, इसलिए उनके बारे में यह कहने में हमें कुछ संकोच नहीं है कि वह किस तरह के आदमी थे और उनकी व्यस्तताएँ क्या थीं। उनकी दिलचस्पियाँ क्या थीं। सब जानते हैं। निस्सन्देह मिर्ज़ा ग़ालिब वैश्विक और मानवीय साहित्य के इतिहास के एक बहुत बड़े शाइर थे, यह अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन उनके कलाम को तसव्वुफ़ का वास्तविक प्रवक्ता क़रार देना बिलकुल दूसरी बात है। हाफ़िज़ का ज़माना चूँकि ज़रा पुराना है, उनकी ज़िन्दगी पर एक धुँध सी छाई हुई है। इसलिए हम नहीं जानते कि उनकी जीवन-प्रणाली क्या थी। मिर्ज़ा ग़ालिब की तरह की थी या वाक़ई अल्लाहवालों की तरह की, यह अल्लाह को मालूम है। लेकिन इस तरह के शाइरों की वजह से बहुत-सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें फैल गईं, और ऐसी धारणाएँ सामने आने लगीं जो अस्ल सूफ़ी लोगों की अभीष्ट नहीं थीं।
उसी ज़माने में यानी छठी शताब्दी हिजरी से लेकर बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी हिजरी तक सूफ़ी लोगों की ‘तज़किरे’ (वृत्तान्त) भी बहुत अधिक लिखे गए। बहुत-से बड़े सूफ़ियों के ‘मलफ़ूज़ात’ (कथन) संकलित किए गए। इन ‘मलफ़ूज़ात’ और ‘तज़किरों’ में बहुत बड़ा हिस्सा अप्रमाणित बातों का है। ख़ुद कुछ बड़े-बड़े और विद्वान सूफ़ी लोगों ने यह बात स्वीकार की है कि ‘मलफ़ूज़ात’ के इस पूरे भंडार में से कोई चीज़ भी ज्ञानपरक रूप से सहीह सूफ़ी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सूफ़ियाना शिक्षाएँ क्या हैं? उनका मूलस्रोत केवल पवित्र क़ुरआन और सुन्नत है, या इस कला के प्रमाणित और विश्वसनीय विशेषज्ञों के (जिनमें से कुछ का मैंने नाम लिया) ज्ञानपरक शोध और दीनी लेख हैं। किसी सूफ़ी का उल्लेख, किसी सूफ़ी के ‘मलफ़ूज़ात’ किसी बड़े-से-बड़े सूफ़ी की यादाशत इन शिक्षाओं का मूलस्रोत नहीं है। ग़लत-फ़हमी की एक और वजह कुछ शब्दावलियाँ भी हैं जिनमें से एक-दो की मैंने निशानदेही की है। एक शब्दावली की मैं और निशानदेही करना चाहता हूँ, जिसको बहुत ग़लत समझा गया और इस ग़लत समझे जाने के कुछ कारण भी हैं, यह ‘फ़ना’ की शब्दावली थी। यह शब्दावली बहुत-से बुज़ुर्गों ने प्रयोग की है। ‘फ़ना’ का शाब्दिक अर्थ तो फ़ना हो जाना, ख़त्म हो जाना या annihilation है। अब अगर यह फ़ना किसी physical अर्थ में हो तो पवित्र क़ुरआन ने इसकी कहीं शिक्षा नहीं दी है। पवित्र क़ुरआन ने कहीं भी यह माँग नहीं की कि इंसान अपने आपको शारीरिक रूप से फ़ना कर ले। इसलिए फ़ना की शब्दावली का शब्दकोशीय अर्थ यहाँ बिलकुल मुराद नहीं है।
जिन लोगों ने उदाहरणार्थ हज़रत मुजद्दिद साहब ने या शाह वलीउल्लाह ने या और लोगों ने ‘फ़ना’ को स्पष्ट किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ‘फ़ना’ से मुराद यह है कि इंसान अपने दिल और रूह को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि उसकी वे तमाम भौतिक और वासनात्मक इच्छाएँ फ़ना (समाप्त) हो जाएँ जो उसकी मनेच्छाओं पर आधारित हैं और शरीअत से टकराती हैं। इन तमाम इच्छाओं को ‘फ़ना’ कर देने का नाम और ऐसी फ़ितरत बना लेने का जिसके परिणामस्वरूप पैग़म्बर के अनुपालन की अपेक्षाएँ स्वाभाविक मामलों की तरह पूरी होने लगें, इस कैफ़ियत को ‘फ़ना’ की शब्दावली से याद किया गया। इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) जिनकी फ़िक़्ह की पैरवी हमारे सऊदी भाई करते हैं, उनके ज़माने से लेकर कमो-बेश सौ साल पहले तक इस फ़िक़्ह के माननेवालों में अनगिनत अहले-तसव्वुफ़ पैदा हुए हैं। हंबली सूफ़ियों में सबसे बड़ा नाम इमाम तसव्वुफ़ शैख़ अब्दुल-क़ादिर जीलानी का है, बल्कि सबसे बड़े सूफ़ी इस रिवायत में ख़ुद शेख़ुल-इस्लाम अल्लामा इब्ने-तैमिया हैं। उनकी दो मोटी-मोटी किताबें जो उनके फ़तवों की दसवीं और ग्यारहवीं जिल्द पर आधारित हैं इस मामले में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। ये दोनों मोटी जिल्दें तमाम-तर तसव्वुफ़ की बातों से भरी पड़ी हैं। उनमें से एक जिल्द का नाम है ‘इल्मुस-सुलूक’ और दूसरी जिल्द का नाम है ‘इल्मुत-तसव्वुफ़’। इन दोनों जिल्दों में ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ के मसलों के बारे में अल्लामा इब्ने-तैमिया ने जो कुछ लिखा है उसमें और शैख़ अहमद सरहिन्दी के लेखों में कोई अन्तर नहीं है। केवल शब्दावलियाँ और वर्णन-शैली का अन्तर है। इब्ने-तैमिया ने अरबी में लिखा है। शैख़ अहमद सरहिन्दी ने फ़ारसी में लिखा है। ग़लत तसव्वुफ़ पर जो आलोचनाएँ इब्ने-तैमिया की हैं वही और वैसी ही आलोचनाएँ शैख़ अहमद सरहिन्दी और शाह वलीउल्लाह की भी हैं। सिवाय भाषा, वर्णन-शैली और शब्दावलियों के अन्तर के इन लोगों के शोध में कोई अन्तर नहीं है। अल्लामा इब्ने-तैमिया ने भी ‘फ़ना’ की शब्दावली को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उसको पसन्द किया है और इसके यही दो अर्थ क़रार दिए हैं। अगर वे किसी शारीरिक ‘फ़ना’ के अर्थ में है तो वह अस्वीकार्य है और उसकी शरीअत ने शिक्षा नहीं दी है, लेकिन अगर वह इच्छाओं को मिटाकर शरीअत के अनुसार बनाने के अर्थ में है तो वह न केवल स्वीकार्य है, बल्कि वह इस्लाम का अभीष्ट और लक्ष्य है।
आजकल आधुनिक काल में तसव्वुफ़ का पुनरुत्थान एक नए अन्दाज़ से हो रहा है, लेकिन इसमें दो पहलू बड़े ख़तरनाक हैं। जहाँ तक मुसलमानों के इस एहसास का सम्बन्ध है कि यह एक सृजनात्मक और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परम्परा थी और बीसवीं शताब्दी की दिन-प्रतिदन बढ़ते भौतिकवाद के माहौल में मुसलमानों का ध्यान इससे हट गया और विभिन्न कारणों के आधार पर इससे पिछले सौ-सवा-सौ साल के दौरान लापरवाही बरती गई, अब इस परम्परा का पनरुत्थान होना चाहिए, यह विवेक तो ख़ुद अपनी जगह अत्यन्त सम्माननीय है। लेकिन इस परम्परा को लम्बे समय से कुछ ग़ैर-मुस्लिम ताक़तें भी अपने राजनैतिक और उपनिवेशवादी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाह रही हैं और कालान्तर में भी उन्होंने इसको प्रयोग करना चाहा। 1971-72 में सोवियत यूनियन ने एक विधिवत पॉलिसी के तहत यह फ़ैसला किया था कि मुस्लिम जगत् में तसव्वुफ़ के नाम पर इन ‘इबाहियत-पसन्द’ (स्वच्छन्दतावादी) चिन्तकों की देख-रेख की जाए जो ‘बातिनीयत’ (रहस्यवाद) के ध्वजावाहक रहे हैं। सच्चाई यह है कि सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद के ज़माने में ‘बातिनियत’ ने तसव्वुफ़ में बड़ी घुसपैठ पैदा की थी, और ‘बातिनियत’ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बातिनी कारिंदे तसव्वुफ़ के लबादों में सामने आए थे। सोवियत यूनियन के कारिंदों का ख़याल था कि इस छिपी हुई विचारधारा को ज़िन्दा किया जाए। आपमें से कुछ लोगों को शायद याद हो कि वहाँ से एक चिन्तक बाबा-जान ग़फ़ूर (मृत्यु 1973 ई॰ में) पाकिस्तान आया था और उसने पूरे एक महीने पाकिस्तान का दौरा किया था और हर जगह तसव्वुफ़ को ज़िन्दा करने की दावत दी थी। यह 1973 ई॰ में इस सोवियत यूनियन की तरफ़ से कोशिश रही है जो धर्म ही को सिरे से स्वीकार नहीं करते थे। अब वे अधर्मी नास्तिक ‘इबाही’ और ‘बातिनी’ तसव्वुफ़ के ध्वजावाहक थे। वह कोशिश अलहमदु लिल्लाह सफल नहीं हुई।
आज की पश्चिमी ताक़तें भी मुस्लिम जगत् में तसव्वुफ़ को ज़िन्दा करना चाह रही हैं। कुछ मुस्लिम देशों में तसव्वुफ़ की चेयर्ज़ क़ायम हो रही हैं। यह मात्र इत्तिफ़ाक़ भी हो सकता है और पश्चिम के उस नुस्ख़े के प्रभाव भी हो सकते हैं, जो पश्चिमवालों ने सोचा है। पिछले दिनों अमेरिकी सी.आई.ए. के सहयोगी और सहकर्मी संस्था रैंड फ़ाउंडेशन (Rand Foundation) की ओर से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें आम मुसलमानों में प्रभाव रखनेवाले गिरोहों की निशानदेही की गई थी। जिन वर्गों का संरक्षण करने का मश्वरा अमेरिकी सरकार को दिया गया था, उनमें अहले-तसव्वुफ़ के कुछ गिरोह भी शामिल थे। वे अहले-तसव्वुफ़ जो बिगड़े हुए तसव्वुफ़ के प्रतिनिधि हों। जो ‘बातिनियत’ से प्रभावित हों और शरीअत और ‘तरीक़त’ की इस व्यापकता का प्रतिनिधित्व न करते हों, जिसके प्रतिनिधि इमाम ग़ज़ाली (रह॰) और शैख़ अहमद सरहिन्दी हैं।
[तसव्वुफ़ के समर्थक यह बता पाने में भी असमर्थ हैं कि इस्लामी ‘शरीअत’ के होते हुए अलग से ‘तरीक़त’ की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या यह शरीअत से बिलकुल अलग कोई चीज़ है? अगर है तो इस्लाम को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर यह शरीअत का ही एक रूप है, तो इसे अलग नाम से पारिभाषित क्यों किया जाता है?———अनुवादक]
बहरहाल यह था सारांश तसव्वुफ़ की उस शिक्षा का जिसको इस्लामी विद्वानों ने एक संकलित ज्ञान और कला के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। यह संकलित ज्ञान या कला जिसको कुछ विद्वानों ने फ़िक़्हुन-नफ़्स के नाम से याद किया है, कुछ और लोगों ने फ़िक़्हे-बातिन के नाम से याद किया है। और ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ जिसका लक़ब क़रार पाया, यह प्रचलित भाषा में तसव्वुफ़ के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक पूर्ण और व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था की प्रतिनिधि है जिसमें नई-नई बातें और अध्याय शामिल हुए। जैसे-जैसे शेष तमाम ज्ञानों में विकास होता गया और नए-नए विषय और नए-नए अध्याय तफ़सीर (टीका), हदीस और कलाम वग़ैरा में शामिल होते गए, उसी तरह फ़िक़्हुल-क़ल्ब में भी वृद्धि होती गई, बहसों और वार्ताओं में नए-नए विषय शामिल होते चले गए और यों यह कला बहुत आरम्भिक आरम्भ में अपनी सादा क़िस्म से बढ़कर एक संकलित और संगठित ज्ञान के रूप में अपनाई गई, जिससे उन तमाम लोगों ने बहस की है, जिन्होंने इस्लामी ज्ञान एवं कलाओं के इतिहास पर या ज्ञान एवं कलाओं के संकलन और वितरण पर लिखा है।
शैख़ अबुल-हसन शाज़ली जो प्रसिद्ध सूफ़ी लोगों में से हैं, उनका कहना है कि तसव्वुफ़ से मुराद वह कला है जिसके द्वारा इंसानी नफ़्स को इबादत के लिए तैयार किया जाए और अल्लाह के आदेशों के अनुपालन के लिए उसको आमादा किया जाए। एक प्रसिद्ध लेखक जिनकी किताब ‘कश्फ़ुज़-ज़ुन्नून’ इस्लामी ज्ञान-विज्ञान के इतिहास में नुमायाँ स्थान रखती है, यानी हाजी ख़लीफ़ा, वे तसव्वुफ़ की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि तसव्वुफ़ से मुराद वह ज्ञान है जिसके द्वारा अहले-कमाल के आध्यात्मिक विकास की कैफ़ियतें मालूम होती हैं और मानवजाति जैसे-जैसे ‘सआदत’ के दर्जों में विकास करती रहती है, इन विकासों का ज्ञान और कैफ़ियतें मालूम होती हैं।
शैख़ुल-इस्लाम ज़करिया अंसारी का कहना है कि तसव्वुफ़ से मुराद वह ज्ञान है जिसके द्वारा ‘तज़किया-ए-नफ़्स’ की कैफ़ियतों का ज्ञान हो। नैतिकता की सुथराई और पाकीज़गी प्राप्त हो और ज़ाहिर और बातिन का निर्माण हो। यह सब काम इस उद्देश्य के लिए हों कि वह शाश्वत ‘सआदत’ और ख़ुशबख़ती प्राप्त हो जाए जो इस्लाम का और तमाम आसमानी धर्मों का वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि इमाम शेरानी ने लिखा है कि तसव्वुफ़ की अस्ल वास्तविकता यह है कि ‘इख़लास’ (निष्ठा) के साथ शरीअत पर अमल करने का रास्ता आसान हो जाए। अत: जो आलिम भी निष्ठा के साथ अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास रखते हुए अपने ज्ञान पर अमल करता है, वही हक़ीक़त में वास्तविक अर्थ में सूफ़ी है।
सूफ़ी की वास्तविकता यही है कि वह आलिम जिसका ज्ञान और कर्म दोनों बराबर हों, न ज्ञान कर्म से ज़्यादा हो, न कर्म ज्ञान से कम या ज़्यादा हो। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान में जितना बढ़ता जाएगा तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ की क्रियाओं में भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि तसव्वुफ़ की परिभाषा करनेवाले तमाम विद्वानों ने तसव्वुफ़ की परिभाषा में नैतिक और आध्यात्मिक पराकाष्ठा के विकास, मानवजाति की ‘सआदत’ में बेहतरी और उन तमाम दर्जों और कमालात (पराकाष्ठाओं) की ‘मारिफ़त’ (पहचान) को बयान किया है जो दरअस्ल सूफ़ियों का अभीष्ट होते हैं।
उपमहाद्वीप के एक ज्ञानवान ने तसव्वुफ़ की इस तरह परिभाषा की है कि वह इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) से जुड़ी फ़िक़्ह की तारीफ़ का एक हिस्सा बन जाए। इमाम साहब ने फ़िक़्ह की परिभाषा करते हुए लिखा था “इंसानी नफ़्स का यह ‘मारिफ़त’ (गहरा इल्म) कि उसको यह पता चल जाए कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और उसके अधिकार क्या हैं? यानी दीनी और शरई वाजिबात और फ़राइज़ का ज्ञान और पहचान, यही वास्तव में फ़िक़्ह है।” इमाम साहब की इस परिभाषा के बारे में विद्वानों का हमेशा से यह कहना रहा है कि इसमें इल्मे-उसूल और इल्मे-फ़ुरूअ यानी इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान), उसूले-फ़िक़्ह और जुज़इयाते-फ़िक़्ह सब शामिल हैं, इसलिए कि नफ़्स की जो ज़िम्मेदारियाँ आध्यात्मिकता के बारे में हैं, उनका ज्ञान भी फ़िक़्ह कहलाता है, इसलिए फ़िक़्ह की परिभाषा जैसा कि इमाम साहब ने की है अत्यन्त व्यापक परिभाषा है, फ़िक़्ह की इस परिभाषा में शरीअत के वे तमाम अध्याय शामिल हैं जिनसे लेक्चर्स के इस सिलसिले में चर्चा की गई है, यानी इंसान के ज़ाहिरी कर्मों से सम्बन्धित आदेश, इंसान के अक़ीदे और ईमानियात और फ़िक्र से सम्बन्धित निर्देश और नैतिक और आध्यात्मिक सुथराई और पवित्रता के बारे में शरीअत का मार्गदर्शन। अगर ऐसा है तो निश्चय ही फ़िक़्ह, विशेष रूप से फ़िक़्हुन-नफ़्स और फ़िक़्हुल-क़ल्ब, उच्चतम ज्ञान में से है, इसलिए कि यह तथ्यों का ज्ञान है, और इस मामले का ज्ञान है जो अल्लाह और बन्दे के दरमियान होता है, जिसके द्वारा आज्ञापालन में ‘इख़लास’ (निष्ठा) पैदा होता है, अल्लाह की ओर ध्यान केन्द्रित होता है।
तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह के दरमियान जो गहरा सम्बन्ध है उसकी ओर कई बार इशारा किया जा चुका है। हज़रत इमाम मालिक (रह॰) से सम्बद्ध वह कथन भी जो अनेक सूफ़ी लोगों ने नक़्ल किया है, हमने देखा, जिसमें इमाम साहब ने फ़रमाया था कि जिस व्यक्ति ने फ़िक़्ह जाने बिना तसव्वुफ़ पर अमल करने की कोशिश की उसके बारे में ख़तरा है कि उसका अंजाम ‘ज़िंदीक़ियत’ (नास्तिकता) पर न हो। इसी तरह से जो व्यक्ति तसव्वुफ़ के बिना फ़िक़्ह के ज़ाहिरी आदेशों पर अमल करना चाहेगा उसके बारे में प्रबल आशंका इस बात की है कि वह उल्लंघन के रास्ते पर चल पड़े।
शरीअत और तसव्वुफ़ या फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के इस गहरे सम्बन्ध के बारे में शायद ही कोई उल्लेखनीय व्यक्ति ऐसा हो जिसने उसको स्पष्ट न किया हो। तसव्वुफ़ के तमाम सम्मानित प्रतिनिधि इस बात पर ज़ोर देते आए हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी, शैख़ अहमद सरहिन्दी (रह॰) ने अपने ‘मक्तूबात’ (पत्रों) में एक जगह लिखा है कि “क़ियामत के दिन शरीअत के बारे में सवाल किया जाएगा, तसव्वुफ़ के नुक्तों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जन्नत में प्रवेश और जहन्नम से मुक्ति शरीअत से जुड़े रहने पर है, शरीअत पर अमल करने पर निर्भर है।” इसलिए यह बात कि शरीअत और तसव्वुफ़ या फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ दोनों एक हैं, यह तसव्वुफ़ के सभी आलिमों के यहाँ सर्वसम्मत समस्या रहा है, एक फ़िक़्हुन-नफ़्स है, दूसरा फ़िक़्हुल-आमाल है। फ़िक़्ह के बिना तसव्वुफ़ बेमानी है। इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति शरीअत के ज़ाहिरी आदेशों पर अमल नहीं कर रहा तो उसका तसव्वुफ़ मात्र एक झूठा दावा है, इसी तरह से तसव्वुफ़ के बिना कोई फ़क़ीह नहीं हो सकता, इसलिए कि जो अमल फ़िक़्ह के आदेशों पर वह कर रहा है, जिसका वह दावेदार है उसमें अगर इख़लास (निष्ठा), सच्चाई और ध्यान नहीं है तो वह बेकार है और यह सच्चाई और ध्यान तसव्वुफ़ के द्वारा पैदा हो सकता है। अगर सिरे से ईमान ही नहीं है तो न फ़िक़्ह है न तसव्वुफ़, इसलिए कि ईमान के बिना ये दोनों अस्वीकार्य हैं। इसलिए कि जैसा कि शैख़ अबुल-अब्बास ज़ुरूक़ ने लिखा है। ये तीनों एक ही चीज़ हैं, अस्ल ईमान है जिसके दो रुख़ हैं, एक ज़ाहिरी रुख़ है जो सबको नज़र आता है, और एक बातिनी (आन्तरिक) रुख़ है जिसका सम्बन्ध इंसान के दिल, नीयत, और रूह से है। यही वजह है कि तसव्वुफ़ के अपने ज़माने के सबसे बड़े इमाम जिनको सैयदुत्ताइफ़ा के लक़ब से याद किया गया है, जुनैद बग़्दादी ने लिखा है कि “हर वह तरीक़ा जिसको शरीअत ने रद्द कर दिया वह ज़ंदक़ा है। इसलिए कि शरीअत एक कुल है और तरीक़त उसका एक अंग है।” एक बुज़ुर्ग ने लिखा है कि “शरीअत दरख़्त है और तरीक़त उसको पानी देने के मुतरादिफ़ है। अगर शरीअत एक जिस्म है तो तरीक़त उसकी ग़िज़ा और दवा है, आम हालात में इसकी हैसियत ग़िज़ा की है और कुछ ख़ास हालात में वह दवा की जगह हो जाती है।” तसव्वुफ़ के कुछ उपायों की हैसियत दवा की भी होती है, यही वजह है कि तमाम बड़े सूफ़ी इसपर ज़ोर देते आए हैं कि एक शैख़े-तरीक़त की मौलिक शर्तों में यह बात शामिल है कि वह शरीअत का भरपूर ज्ञान रखता हो। जो व्यक्ति शरीअत का पूरा ज्ञान नहीं रखता वह एक निष्ठावान मुसलमान तो शायद हो सकता है, लेकिन शैख़े-तरीक़त और प्रशिक्षक नहीं हो सकता।
शैख़-तरीक़त और निपुण प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी है कि वह शरीअत के आदेशों पर अमल करता हो। शैख़ अब्दुल-वह्हाब शेरानी ने अपनी किताब ‘अनवारे-क़ुदसिया’ में लिखा है कि एक समय के शैख़ की निशानी यह है कि वह क़ुरआन और सुन्नत का गहरा ज्ञान रखता हो, इन दोनों के तमाम आदेशों पर खुले और छिपे दोनों स्थितियों में अमल करता हो, अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करता हो, अल्लाह और बन्दे के दरमियान जो अह्द (वचन) है उसको पूरा करता हो, तक़्वा (ईशपरायणता) के मामले में किसी बहाने का सहारा न लेता हो, अपने तमाम मामलों में सावधानी और शरीअत के मामले में अत्यन्त सावधानी से काम लेता हो, मुसलमानों के साथ उसका व्यवहार स्नेहमयी हो, किसी गुनहगार से घृणा न करता हो, इंसानों से नर्मी से पेश आता हो, गुनहगार मुसलमानों के लिए रहमत और ख़ैर की दुआ करता हो, उसकी दानशीलता हर एक के लिए, गुनहगार और भल लोगों सबके लिए खुली हो, शुक्रगुज़ार और नाशुक्रगुज़ार सबके साथ उसका रवैया एक जैसा हो, अल्लाह की मख़लूक़ को वह अपने परिवार की तरह अपनी ज़िम्मेदारी समझता हो, ऐसा व्यक्ति जब भी मौजूद होगा तो वह निश्चय ही संसार के मामले में ज़ुह्द (परहेज़गारी) और इस्तिग़ना (निस्पृहता) से काम लेता होगा, तन्हाई को पसन्द करता होगा, शोहरत और प्रोपेगंडे से नफ़रत करता होगा, उसके तमाम काम क़ुरआन और सुन्नत के अनुसार होंगे, उसका वह फ़रिश्ता जो बाएँ तरफ़ निर्धारित है और उसके गुनाहों को लिखने का पाबन्द है उसके पास लिखने को कुछ होगा ही नहीं, इसलिए कि उसका समय सारा-का-सारा भले कर्मों में लगा होगा, बर्बाद करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं होगा। उस दौर के फ़ुक़हा और नेक लोग उसकी ख़ूबियों के गवाह होंगे और विशेष रूप से उसको समय के किसी प्रमाणित शैख़ ने इसकी अनुमति दी हो कि वह जनसाधारण के प्रशिक्षण का कर्त्तव्य अंजाम दे।
[ऊपर शैख़े-तरीक़त के जो गुण और जो शर्तें बताई गई हैं, लगभग वे सारी बातें हर मुसलमान में होनी चाहिएँ, इन्हें शैख़े-तरीक़त के साथ ख़ास करने की या इन गुणों के व्यक्ति को शैख़े-तरीक़त कहने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, आख़िर में जो यह शर्त लगाई गई कि उसे जनसाधारण का प्रशिक्षण करने के लिए किसी ‘प्रमाणित’ शैख़ की ‘अनुमति’ दरकार होगी, यह विचारणीय है। अव्वल तो किसी शैख़ को प्रमाणित कैसे माना जाए? यही एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। उसे प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से होगा और इस प्रमाणपत्र की ज़रूरत क्यों है? इन सवालों के जवाब तसव्वुफ़ के समर्थकों के पास नहीं हैं। दूसरे आम मुसलमानों का प्रशिक्षण करने के लिए किसी प्रमाणित शैख़ की ‘अनुमति’ क्यों? जबिक अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आदेश है, “पहुँचा दो मेरी तरफ़ से, चाहे एक ही आयत (क्यों न आती) हो।” (सहीह बुख़ारी-3461) यानी जिसको जितना इस्लाम का ज्ञान है वह उसे दूसरों तक पहुँचा दे। इसमें उसे किसी से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती।———अनुवादक]
हज़रत शैख़ अहमद सरहिन्दी ने एक जगह लिखा है कि हमारे ज़माने के जो सूफ़ियाने-ख़ाम (ख़राब सूफ़ी) हैं ये अपने कमज़ोर बहानों के अमल को तरह-तरह के बहानों से, तरह-तरह की मनमानी व्याख्याओं से दुरुस्त साबित करना चाहते हैं, उन्होंने नाच-रंग को अपनी मिल्लत और अपना दीन क़रार दे दिया है, यह ख़ुराफ़ात और खेल-कूद को अपनी इबादत समझते हैं, जो व्यक्ति हराम काम को अच्छा समझता हो वह मुसलमानों की कैटेगरी से निकल जाता है, उसकी गिनती मुर्तदों (इस्लाम से फिर जानेवालों) में होती है। अत: यह समझ लेना चाहिए कि नाच-रंग की महफ़िलों को अच्छा समझना और उनको आज्ञापालन और इबादत का एक प्रकार समझना बहुत बुरी बात है।
[यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि ‘वास्तविक सूफ़ी’ कौन है और कौन ‘ख़राब सूफ़ी’ है, इस झमेले में पड़ने की और इसके नियम एवं सिद्धान्त निर्धारित करने की ज़रूरत क्या है? क़ुरआन और हदीस में स्पष्ट आदेश मौजूद हैं कि हर मुसलमान के लिए क्या सही है और क्या ग़लत। इन आदेशों को काफ़ी क्यों नहीं समझा गया? शरीअत के मार्गदर्शन को पर्याप्त क्यों नहीं समझा गया और ‘तरीक़त’ के नाम पर एक अलग ‘पैकेज’ क्यों तैयार किया गया?]
‘तज़किया-ए-नफ़्स’ जो तसव्वुफ़ का दूसरा नाम है और तसव्वुफ़ का सर्वप्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है इसका प्राप्त करना आसान काम नहीं है। क्या वाक़ई किसी के नफ़्स का ‘तज़किया’ हो चुका है? यह जानना ख़ुद अपनी जगह एक मुश्किल काम है। इंसानी नफ़्स बहुत चालाक और अय्यार है, वह बुद्धि की तरह है जो सौ भेस बना लेती है, इसलिए नफ़्स में तरह-तरह के बहकावे भी पैदा होते हैं, प्रेरक भी इसमें पैदा होते हैं, तरह-तरह के घमंड भी नफ़्स करता है, इसलिए यह जानने के लिए कि क्या वाक़ई ‘तज़किया’ नफ़्स हो गया है? यह देखना चाहिए कि क्या बन्दे ने तौबा कर ली है, क्या वह वास्तविक अर्थों में तौबा कर चुका है, अगर बन्दा वास्तविक अर्थों में तौबा कर चुका है तो फिर उसको तौबा के दर्जों पर कारबन्द होना चाहिए। तौबा का सबसे पहला दर्जा इस कला के विशेषज्ञों के नज़दीक बड़े गुनाहों से तौबा है, फिर छोटे गुनाहों से तौबा, फिर मकरूहात से तौबा वग़ैरा एक लम्बा सिलसिला है। यही वजह है कि इस्लाम के बड़े विद्वान अपने पिछले जीवन पर हमेशा लज्जित रहते और तौबा करते रहते थे। इसलिए कि आगे के आध्यात्मिक विकास और ऊँचे दर्जों के मुक़ाबले में जब वह पिछले दर्जों को देखते थे तो उनको बहुत कम मालूम होते थे। इस पस्ती में उनका कितना समय गुज़रा, मौजूदा ऊँचाई से कब तक महरूम रहे और कितना महरूम रहे, इस महरूमियत की वजह से वे तौबा करते थे और बार-बार अपने अतीत पर ग्लानि का प्रदर्शन किया करते थे।
लेकिन ये अहवाल और मक़ामात जिनकी कोई इंतिहा नहीं है, जो असीमित हैं, यह सब आभासी मामले हैं, उनका सम्बन्ध आन्तरिक अनुभव से है, शब्दों और इबारत से उनकी वास्तविकता को पूरी तरह स्पष्ट करना सम्भव नहीं है [इसकी ज़रूरत भी नहीं है———अनुवादक]। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उन दर्जों और अहवालो-मक़ामात को प्राप्त करना चाहता हो तो इसका तरीक़ा यह है कि वह लगातार कोशिश में लगा रहे यहाँ तक कि ख़ुद महसूस कर ले और उसको अनुभव हो जाए कि दर्जे और अहवालो-मक़ामात क्या हैं?
[और यही तसव्वुफ़ की बुनियादी ख़राबी है, जो उसे इस्लाम से अलग करती और उसे इस्लाम के समानान्तर एक अलग दर्शन बना देती है, जिसके तहत यह कहा जाता है कि इनसान ख़ुद महसूस कर लेता है कि वह अब किस ‘मक़ाम’ पर पहुँच गया है। इस तरह के आभास न तो इस्लाम के निकट कोई महत्त्व रखते हैं, न इस्लाम में अभीष्ट हैं। इस्लाम के निकट बन्दा केवल क़ुरआन में वर्णित अल्लाह के आदेशों के अनुपालन का पाबन्द है और उन आदेशों पर किस तरह अमल किया जाए, इसके लिए वह अल्लाह के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत (तरीक़े) का पाबन्द है। बन्दे का काम यह देखना है ही नहीं कि अब वह किस ‘मक़ाम’ पर पहुँच गया है, बल्कि उसे सारा जीवन बस अल्लाह और रसूल का अनुपालन करना है। रहा परिणाम तो वह उसे आख़िरत में ही मिलेगा, जबिक तसव्वुफ़ का दर्शन सब कुछ इसी दुनिया में आभास कराने का दावेदार है, जो कि इस्लामी धारणाओं के बिल्कुल विरुद्ध है———अनुवादक]
Recent posts
-

इस्लामी शरीअत का भविष्य और मुस्लिम समाज का सभ्यता मूलक लक्ष्य (शरीअत : लेक्चर# 12)
02 December 2025 -
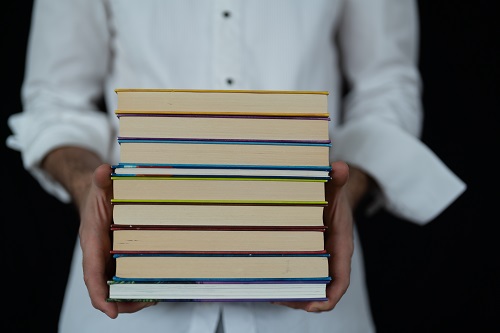
इस्लामी शरीअत आधुनिक काल में (शरीअत : लेक्चर# 11)
25 November 2025 -

इल्मे-कलाम अक़ीदे और ईमानियात की ज्ञानपरक व्याख्या एक परिचय (शरीअत : लेक्चर# 10)
21 November 2025 -

अक़ीदा और ईमानियात - शरई व्यवस्था का पहला आधार (शरीअत : लेक्चर# 9)
17 November 2025 -

तदबीरे-मुदन - राज्य और शासन के सम्बन्ध में शरीअत के निर्देश (शरीअत : लेक्चर# 7)
05 November 2025 -

इस्लाम में परिवार की संस्था और उसका महत्त्व (शरीअत : लेक्चर# 6)
24 October 2025