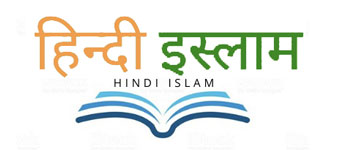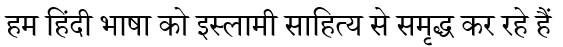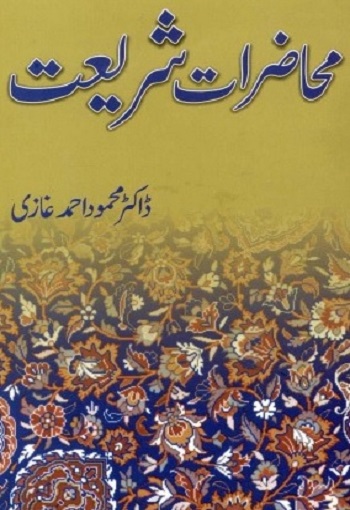
नैतिकता और नैतिक संस्कृति (शरीअत : लेक्चर # 4)
-
शरीअत
- at 31 August 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
इस्लामी शरीअत नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित एक व्यापक जीवन-व्यवस्था है, जो कानून, नैतिक निर्देशों और सांस्कृतिक शिक्षाओं को एकीकृत करती है। डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी के इस लेक्चर में, शरीअत की नैतिक नींव, व्यक्ति से लेकर समाज और मानवता तक के दायरों का विश्लेषण किया गया है। लेक्चर में फ़िक़्ह, इल्मे-कलाम, सूफ़ीवाद और दर्शन जैसी प्रवृत्तियों के माध्यम से नैतिक पराकाष्ठा, इबादत, ज़ब्ते-नफ़्स और चरित्र निर्माण पर चर्चा की गई है। क़ुरआन और सुन्नत की रौशनी में, यह लेख इस्लाम को एक पूर्ण पैराडायम के रूप में प्रस्तुत करता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करता है तथा नैतिक पतन से बचाव के सिद्धांत बताता है। यह मुस्लिम विद्वानों की विरासत को उजागर करता है, जो जीवन की एकता पर जोर देती है। -संपादक
इस्लामी शरीअत का हर विद्यार्थी इस वास्तविकता से पूरे तौर पर परिचित है कि शरीअत के आदेशों का आधार अक़ीदों (धार्मिक अवधारणाओं) और आध्यात्मिक मूल्यों पर है। शरीअत के तमाम सामूहिक नियम, क़ानूनी आदेश, व्यावहारिक निर्देश और सांस्कृतिक शिक्षाओं के हर-हर अंग का अक़ीदों और आध्यात्मिक पवित्रता से प्रत्यक्ष रूप से और गहरा सम्बन्ध है। एक पश्चिमी विद्वान ने इस सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शरीअत ने नैतिक सिद्धान्तों और आध्यात्मिक निर्देशों को क़ानूनी रूप दे दिया है। इस्लामी शरीअत में क़ानून और नैतिकता एक ही वास्तविकता के दो पहलू या एक ही सिक्के के दो रुख़ हैं। इस्लाम का हर क़ानून किसी-न-किसी नैतिक उद्देश्य या आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। इसी तरह इस्लाम की शिक्षा में कोई नैतिक निर्देश ऐसा नहीं दिया गया जिसपर कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक नियम उपलब्ध न किए गए हों। शरीअत के पूरे पुस्तक भंडार में कोई ऐसा इशारा नहीं मिलता जिसके अनुसार क़ानून और फ़िक्ह से असम्बद्ध रहकर आध्यात्मिक दर्जे प्राप्त किए जा सकते हों।
क़ानून और नैतिकता, आध्यात्मिकता और सभ्यता एवं संस्कृति सब के मध्य इस गहरे आपसी सम्पर्क की वजह यह है कि शरीअत मात्र कोई क़ानूनी व्यवस्था नहीं, न यह मात्र कुछ धार्मिक रस्मों का संग्रह है। न यह कुछ नैतिक निर्देश तक सीमित है। इस्लामी शरीअत तो एक ऐसा व्यापक आदर्श या पैराडायम (paradigm) है जो न केवल मानव जीवन को एक नया आयाम प्रदान करता है, बल्कि ये आदर्श पूरे मानव जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर क़ायम करता है, और मानवता के नवनिर्माण की इस प्रक्रिया में ज़िन्दगी के हर पहलू से सम्बन्धित नियम एवं सिद्धान्त उपलब्ध करता है। इन नियमों एवं सिद्धान्तों की रौशनी में जब भी व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन का पुनर्गठन होगा तो इस प्रक्रिया से ज़िन्दगी के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक और सार्थक परिवर्तन जन्म लेंगे। इन परिवर्तनों के नतीजे में समाज, सभ्यता, नैतिकता और संस्कृति की नई-नई निशानियाँ, नए-नए अन्दाज़ और नई-नई शैलियाँ पैदा होंगी। यही वजह है कि बहुत-से चिन्तकों और विद्वानों ने इस्लाम को एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था की शब्दावली से याद किया है। इस शब्दावली का यह अर्थ नहीं है कि इस्लाम ने इंसानों को नियमों के अन्दर कस दिया है, या मानव-बुद्धि की भूमिका को समाप्त कर दिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस्लाम ने ज़रूरी, मौलिक और सैद्धान्तिक निर्देश दे दिए हैं। ऐसे निर्देश जिनकी रौशनी में हर ज़माने और हर इलाक़े के इंसान अपनी-अपनी आवश्यकताओं और अपने-अपने हालात के लिहाज़ से व्यावहारिक विवरण तैयार कर सकते हैं।
कुछ आधुनिकतावादी पूर्ण जीवन-व्यवस्था की इस शब्दावली से सहमत नहीं हैं। वे इससे मतभेद करते हैं और इस्लाम के लिए पूर्ण जीवन-व्यवस्था की शब्दावली स्वीकार और प्रयोग करने में संकोच महसूस करते हैं। इस संकोच की एक बड़ी वजह इस वैचारिक वातावरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो पश्चिमी धर्म-विरोधियों ने पिछले सौ वर्षों के दौरान फैला दिया है। जिसके अनुसार धर्म का कार्यक्षेत्र दिन-प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है। अगर किसी चीज़ को स्वीकार करने में पहले दिन ही से संकोच हो तो इस संकोच के कारण तराश लेना या औचित्य उपलब्ध कर लेना मानव-बुद्धि के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हर नकारात्मक-से-नकारात्मक चीज़ के औचित्य में लुभावने कारण और उत्प्रेरक पेश किए जा सकते हैं। मानव-बुद्धि कमज़ोर-से-कमज़ोर राय के पक्ष में तर्कों का अंबार खड़ा कर देने की कला में बहुत दक्ष है। मानव मस्तिष्क इस मामले में बहुत सक्रिय होता है। वह अपने हित की ख़ातिर हर चीज़ का औचित्य पैदा कर लेता है।
अगर इस्लाम के इतिहास के पूरे भंडार पर एक नज़र डाली जाए, मुसलमानों के बौद्धिक विरासत का एक सरसरी जायज़ा भी लिया जाए तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि मुसलमान बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने इस चौदह सौ साल के लम्बे समय में किस ढंग से मानव जीवन को देखा, व्यक्ति को, ख़ानदान को, समाज को, मुस्लिम समाज को और इस्लामी राज्य और उसके क़ानून को किस अन्दाज़ से संकलित किया। इस्लाम के बौद्धिक, वैचारिक और धार्मिक इतिहास की रौशनी में यह बात बिना किसी संकोच और झिझक के कही जा सकती है कि इस्लाम ने एक ऐसा जीवन सिद्धान्त उपलब्ध किया है जो ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है और जीवन के हर क्षेत्र को अपनी रौशनी से जगमग करता है। अत: यह शब्दावली कि इस्लाम एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है वास्तविकता के बिलकुल अनुसार है। यह शब्दावली इस्लाम की व्यापकता और इस्लाम की विशालता को पूर्ण रूप से बयान करती है।
इस्लामी शरीअत ने व्यक्ति, परिवार, समाज यानी मुस्लिम समाज और राज्य के इन चारों दायरों के साथ-साथ पाँचवें दायरे यानी पूरी मानवता को भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है। इन पाँचों दायरों में मानव जीवन का कोई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके बारे में शरीअत ने कुछ सैद्धान्तिक और मौलिक निर्देश न दिए हों और इस्लामी चिन्तकों ने इन निर्देशों को अपनी-अपनी खोज के अनुसार संकलित न किया हो। जिन लोगों ने शरीअत का अध्ययन विशुद्ध फ़िक़्ह और क़ानून के दृष्टिकोण से किया उन्होंने व्यक्ति को एक सामर्थ्यवान इंसान के तौर पर देखा, एक ऐसा इंसान जिसपर शरई ज़िम्मेदारियाँ आ पड़ती हैं और जो ‘तकलीफ़ाते-शरईया’ (शरीअत द्वारे डाली गई ज़िम्मेदारियों) का विषय और पात्र बनता है। इन लोगों की एक हज़ार साल से अधिक समय पर आधारित रचनाओं के परिणाम फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह की किताबों में सुरक्षित हैं।
कुछ लोगों ने इंसान को इस हैसियत से देखा कि वह सोचने-समझनेवाला एक अस्तित्व है। जिसको बुद्धि की दौलत से माला-माल किया गया है। बुद्धि ही की वजह से वह दूसरे प्राणियों से अलग है। दूसरे प्राणियों पर वह अपनी वैचारिक एवं व्यावहारिक स्वतंत्रता ही की वजह से विशिष्टता और श्रेष्ठता रखता है। इसलिए इन लोगों ने इस पहलू से शरीअत की सम्बन्धित शिक्षा और निर्देशों को स्पष्ट किया। उनकी दिलचस्पी का मैदान व्यावहारिक आदेशों और प्रतिदिन की ज़िन्दगी की समस्याएँ नहीं, बल्कि जीवन की आधारभूत समस्याएँ, अक़ीदे और इस्लामी विचारधारा के मौलिक सिद्धान्त थे। इन लोगों ने अपने ज्ञानपरक प्रयासों को अक़ीदा, तर्कशास्त्र और शरीअत के दर्शन की किताबों में संकलित किया।
कुछ और लोगों ने इंसान को एक ऐसे आध्यात्मिक अस्तित्व के तौर पर देखा जिसके अन्दर तरह-तरह की भावनाएँ और अनुभूतियाँ हिलकोरें लेती रहती हैं। जिसके अन्दर शारीरिक माँगों के साथ-साथ आध्यात्मिक माँगें और प्रवृत्तियाँ भी डाली गई हैं, जो मामलों को विशुद्ध आन्तरिक ढंग में देखता है और आन्तरिक अनुभव के प्रभाव को बहुत महत्त्व के साथ महसूस करता है। उन्होंने आन्तरिक और आध्यात्मिक ढंग से व्यक्ति और समाज के मामलों को देखा। कुछ और लोगों ने विशुद्ध दार्शनिकतापूर्ण और बौद्धिक दृष्टिकोण से इंसान को देखा और उसको एक चिन्तक पशु पाया। उन्होंने एक तुलनात्मक ढंग से शरीअत की इन शिक्षाओं को देखा और अपने वैचारिक निष्कर्ष को संकलित किया।
इस तरह दूसरी शताब्दी हिजरी के अन्त से शरीअत के अध्ययन की ये चार प्रवृत्तियाँ सामने आईं। एक प्रवृत्ति, जिसके प्रतिनिधि प्रतिष्ठित फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्री) थे, उन्होंने फ़िक़ही अन्दाज़ से उन सारे मामलों को देखा। फ़िक़्ह के वे सारे भंडार और किताबें जो हम तक पहुँची हैं वे इसी समझ से भरी हुई हैं। इसी समझ के परिणामों को मानव इतिहास के लाखों बेहतरीन दिमाग़ों ने एक संगठित ढंग से संकलित करके पेश किया। जिन लोगों ने इंसान को एक समर्थ और एक निश्चयवान प्राणी के तौर पर देखा, ये मुतकल्लिमीने-इस्लाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करनेवाले विद्वानों) की जमाअत थी। उन्होंने इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) के दृष्टिकोण से व्यक्ति की ज़िम्मेदारियाँ बयान कीं, इसी दृष्टिकोण से ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों को देखा और समझा। इसी दृष्टिकोण से समाज, राज्य और इंसानियत को देखा। मुतकल्लिमीने-इस्लाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करनेवालों) ने अपने वैचारिक परिणामों को इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की शब्दावलियों में बयान किया। लेकिन इल्मे-कलाम की ये शब्दावलियाँ दरअस्ल शरीअत ही के इस आदर्श या पैराडायम की एक विशेष अन्दाज़ की व्याख्या हैं, वह अन्दाज़ जो वास्तविकता को एक विशुद्ध बौद्धिक और कलामी (तार्किक) दृष्टिकोण से देख रहा हो।
तीसरी प्रवृत्ति सूफ़ियों की है जिन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, मुस्लिम समुदाय, राज्य और मानवता को विशुद्ध आध्यात्मिकता और नैतिक प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से जाँचा। उनके ज़ेहन में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह शुभ कथन था कि “मैं नैतिकता की परिपूर्णता की पूर्ति के लिए भेजा गया हूँ।” अब अगर इंसान के अस्तित्व का उद्देश्य नैतिक पराकाष्ठा की प्राप्ति और उसकी पूर्णता है, अगर अल्लाह के रंग में रंग जाना इंसानों का मूल लक्ष्य है तो फिर इस बात की ज़रूरत थी कि विद्वानों का एक वर्ग ऐसा हो जो इंसान और इंसानी माँगों पर इस दृष्टिकोण से ग़ौर करे।
कुछ और लोग थे जिन्होंने अपने ज़माने के प्रचलित बौद्धिक पैमानों और तर्कों से काम लिया, और विशुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से एक तुलनात्मक ढंग से पूरब और पश्चिम की धारणाओं का आकलन करते हुए इस ढंग से इस्लाम के दृष्टिकोण को पेश करने का प्रयास किया कि बौद्धिकता का कोई पूर्वी या पश्चिमी विद्यार्थी शरीअत के दृष्टिकोण को बौद्धिक दृष्टि से अस्वीकार्य या कम स्वीकार्य क़रार न दे सके। इन लोगों ने अपने दौर की प्रचलित ज्ञानपरक और बौद्धिक धारणाओं की रौशनी में इस्लाम के दृष्टिकोण को बयान किया और अपने ज़माने की दार्शनिक शब्दावलियों में शरीअत को बयान करने की कोशिश की।
ये वे बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ हैं जिनके अनुसार विद्वानों की नस्लों की नस्लें कमो-बेश एक हज़ार वर्ष व्यस्त रहीं। इस तरह यह विशाल और गूढ़ इस्लामी लिटरेचर तैयार हुआ जो आज हमारे सामने है। इस्लामी विद्वानों ने व्यक्ति पर भी बात की है, परिवार पर भी चर्चा की है, समाज, संस्थाओं और हुकूमत को भी शोध का विषय बनाया है। उन्होंने इन सब चीज़ों को इस तरह से एक संगठित और संकलित ज्ञानपरक ढंग से पेश किया है कि ज्ञान की एकता की इस्लामी धारणा नज़रों से ओझल न हो।
पवित्र क़ुरआन ने जब तौहीद का मूल अक़ीदा पेश किया, जो सृष्टि की सबसे बड़ी वास्तविकता है, जो अल्लामा इक़बाल के शब्दों में इस सृष्टि की सबसे बड़ी ज़िन्दा ताक़त है, तो उसी लम्हे से यह अक़ीदा इस्लाम की सारी शिक्षा, शरीअत के सारे आदेशों और धारणाओं और इस्लामी सभ्यता के तमाम पहलुओं का आधार क़रार पाया। इस दृष्टिकोण से जब सृष्टि के तथ्यों का अध्ययन किया गया तो उन बज़ाहिर बिखरे हुए तथ्यों में एक ऐसी अनिवार्य एकता का रहस्योद्घाटन हुआ जो मानव जीवन के तमाम क्षेत्रों को परस्पर जोड़ती और संगठित करती है। बज़ाहिर इस्लामी विद्वानों ने ज्ञान का विभाजन अक़्ली (बौद्धिक) और नक़्ली (क़ुरआन और हदीस से प्राप्त ज्ञान) के हिसाब से किया है। उलूमे-नक़्लिया वे हैं जो या तो प्रत्यक्ष रूप से क़ुरआन और हदीस में लिखे हैं या उनसे लिए गए सिद्धान्तों और नियमों पर आधारित हैं। और उलूमे-अक़्लिया वे हैं जो इंसानों ने अपनी, बुद्धि, अनुभव और अवलोकन से खोज करके संकलित किए हैं। लेकिन यह विभाजन मात्र विद्वार्थियों के समझाने के लिए है। ये ज्ञान-विज्ञान के इस अथाह समुद्र को इंसानों के ज़ेहन के क़रीब बनाने के लिए ये शब्दावलियाँ प्रयोग की गईं। इस विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि इस्लामी विद्वानों की राय में इन दोनों प्रकार के उलूम में कोई टकराव या किसी प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है, या दोनों ऐसी समानान्तर रेखाओं की हैसियत रखते हैं जो एक-दूसरे से आज़ाद और तटस्थ होकर सफ़र कर रही हों, जिनका एक-दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो। इसके विपरीत ये तमाम ज्ञान-विज्ञान एक ऐसे कुल (पूर्णता) की विभिन्न आंशिक निशानियाँ हैं जो वास्तविकता के विभिन्न क्षेत्रों पर रौशनी डालती हैं और वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद देती हैं।
इस दृष्टिकोण से शरीअत को देखा जाए तो यह बात पहली नज़र ही में स्पष्ट हो जाती है कि पूरी इस्लामी शरीअत एक सबसे अलग और एकजुट इकाई है। जैसा कि शरीअत का हर विद्यार्थी जानता है कि इस्लामी शरीअत मानव जीवन के तमाम आधारभूत मामलों से बहस करती है। मसलन अगर आप फ़िक़्ह की कोई किताब उठाकर देखें तो आपको उसमें सबसे पहले विशुद्ध व्यक्तिगत मामलात उदाहरणार्थ तहारत और पाकीज़गी के मसाइल (विस्तृत आदेशों) से बहस मिलेगी। सुबह उठकर इंसान स्नानगृह में पाकी प्राप्त करता है। यह उसका विशुद्ध निजी मामला है। आज की प्रचलित धारणाओं की रौशनी में यह किसी सामूहिक बहस का या बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए कि यह हर व्यक्ति का अत्यन्त निजी मामला है। लेकिन शरीअत और फ़िक़्हे-इस्लामी की एकता इस बात की माँग करती है कि तहारत और पाकीज़गी की समस्याएँ भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हों जो जीवन के शेष भागों को संगठित करती है। जो फ़िक़्हे-इस्लामी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, वही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है, इसी से राज्य का फ़ौजदारी क़ानून संकलित होता है, जिसकी रौशनी में राज्य का दीवानी क़ानून और आर्थिक मामले संकलित होते हैं। ज़रूरी है कि इसी मार्गदर्शन व्यवस्था की रौशनी में ये सब सिद्धान्त संकलित किए जाएँ।
इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की तरह सूफ़ियों और मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने भी ज्ञान के इस एकत्व को बरक़रार रखते हुए वास्तविकता की वह व्याख्या की जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, मुस्लिम उम्मत, राज्य और पूरी मानवता का नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण एक ऐसी व्यवस्था के तहत किया जा सके जिसका आधार एक हो, मंज़िले-मक़्सूद (गन्तव्य) एक हो, जिसमें इंसानों को एक इकाई और मानवता को एक एकत्व के तौर पर देखा और समझा गया हो। यही कैफ़ियत मुतकल्लिमीने-इस्लाम की है। यही कैफ़ियत सूफ़ियों की है और यही कैफ़ियत इस्लामी दार्शनिकों की है।
चूँकि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) इंसान के ज़ाहिर से ज़्यादा बहस करते हैं, इसलिए उनका ध्यान फ़िक़्ह के उन पहलुओं पर केन्द्रित रहा जिनका सम्बन्ध ज़ाहिरी आमाल और इंसान के शारीरिक अंगों से है। इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, ज़कात अदा करता है, शादी ब्याह के सम्बन्ध बनाता है, क्रय-विक्रय करता है, लेन-देन करता है, व्यापार करता है, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हिस्सा लेता है, यह सब उसके जीवन के ज़ाहिरी कर्म हैं। लेकिन उनमें से हर ज़ाहिरी कर्म के पीछे एक आन्तरिक प्रेरक, आन्तरिक भावना या आन्तरिक क्रिया भी पाई जाती है, जिसका सम्बन्ध इंसान की नीयत, उसके इरादे और दूसरे उत्प्रेरकों से होता है। कोई ज़ाहिरी काम ऐसा नहीं है जिसके पीछे एक छिपा हुआ प्रेरक और भावना मौजूद न हो। यही वजह है कि क़ुरआन के कुछ टीकाकारों ने लिखा है (जिसको बहुत-से लोगों ने ग़लत समझा या जान-बूझकर ग़लत समझाना चाहा) कि पवित्र क़ुरआन के हर आदेश का एक ज़ाहिर और एक बातिन (आन्तरिक अर्थ) है। यह ज़ाहिर और बातिन किसी दार्शनिक या सांकेतिक अर्थ में या किसी ऐसे अर्थ में नहीं है कि जो शरीअत के विद्वानों की नज़र में न हो, या इस्लाम के सर्वप्रथम सम्बोधकों ने, प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन ने, इसको न समझा हो। बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि पवित्र क़ुरआन के हर आदेश का एक ज़ाहिरी पहलू है जो इंसान के शारीरिक अंगों से सम्बन्ध रखता है, दूसरा पहलू वास्तविक और आन्तरिक पहलू है जो इंसान की भावना, नीयत और प्रेरक तत्त्वों से सम्बन्ध रखता है। इस दृष्टि से जब हम व्यक्ति के प्रशिक्षण, आन्तरिक सुधार और आध्यात्मिक माँगों का जायज़ा लेते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि व्यक्ति के आन्तरिक सुधार और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा से मुराद नैतिक दर्शन की वैचारिक समस्याएँ और बहसें नहीं, बल्कि इससे मुराद वह नैतिक पराकाष्ठा पैदा करना है जिनकी जगह-जगह क़ुरआन और सुन्नत में शिक्षा दी गई है। इस उच्च नैतिक आचरण से व्यवहारतः विभूषित होने के लिए अल्लाह से सम्बन्ध और आख़िरत की जवाबदेही का एहसास मौलिक हैसियत रखता है।
प्रशिक्षण के मामले में सबसे पहले व्यक्ति और परिवार के महत्त्वपूर्ण विषय आते हैं, जिनके प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण के बारे में आज कुछ बातें प्रस्तुत हैं। व्यक्ति के बाद एक मैदान इस चर्चा का मुस्लिम उम्मत और समाज है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। और दूसरा मैदान वह है जिसको मुतकल्लिमीने-इस्लाम और इस्लाम के दार्शनिकों ने ‘तदबीरे-मदन’ के शीर्षक से याद किया है। इन सब लोगों ने, बल्कि बहुत-से सूफ़ियों ने, जिनमें इमाम ग़ज़ाली और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी शामिल हैं, तमाम मुतकल्लिमीन और इस्लामी दार्शनिकों ने इन सब मामलों को ‘हिकमत’ (तत्त्वदर्शिता) के एक सारगर्भित शब्द के तहत बयान किया है। यानी ‘हिकमत’ का वह मूलस्रोत जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से फूटा है, यह मानव जीवन के तमाम विभागों को सिंचित करता है। इंसानियत के तमाम विभाग इससे रौशन और लाभान्वित होते हैं। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रशिक्षित न हो और व्यक्ति इस अन्दाज़ से प्रशिक्षण पाकर सामने न आए जो इस्लाम को दरकार है, वह इस परिवार का गठन नहीं कर सकता जिस परिवार का गठन इस्लाम का लक्ष्य है। जब तक ऐसे दरकार और आदर्श लोग और परिवार प्रभावकारी और उल्लेखनीय संख्या में मौजूद न हों उस समय तक वह समाज या मुस्लिम समुदाय अस्तित्व में नहीं आ सकता जो पवित्र क़ुरआन का सर्वप्रथम और अति महत्त्वपूर्ण सामूहिक लक्ष्य है।
यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझने की है कि पवित्र क़ुरआन का सबसे मौलिक और महत्त्वपूर्ण सामूहिक लक्ष्य मुस्लिम ‘उम्मत’ की स्थापना है। जिसके लिए पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह आदेश भी दिया है, ख़बर भी दी है और भविष्यवाणी भी की है। इस मुस्लिम ‘उम्मत’ की विशिष्टताएँ भी बयान की हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बयान की हैं और इसके कर्त्तव्यों की निशानदेही भी की है। मुस्लिम ‘उम्मत’ जब अस्तित्व में आ जाए तो उसकी सुरक्षा, उसके बचाव के लिए और उसकी ओर से कुछ मौलिक कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने के लिए राज्य की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मुतकल्लिमीने-इस्लाम और इस्लामी दार्शनिक और बहुत-से सूफ़ियों ने इन तीनों विषयों को इसी क्रम से बयान किया है। सबसे पहले व्यक्ति का प्रशिक्षण, उसके बाद परिवार का गठन, फिर राज्य की स्थापना और गठन। आज की प्रारम्भिक चर्चा के बाद इन तीनों विषयों पर इसी क्रम से चर्चा होगी।
जब हम नैतिकता और नैतिकता संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे सामने व्यक्ति का नैतिक चरित्र रहता है। ज़ाहिर है कि ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए कि नैतिक ज्ञान का उद्देश्य अगर व्यक्ति का नैतिक प्रशिक्षण नहीं तो फिर वह एक निरा दर्शन है जिससे इस्लाम को ग़रज़ नहीं है। इस्लाम की दिलचपसी क्रिया से है विशुद्ध वैचारिक ज्ञान और केवल वैचारिकता से नहीं, फिर जब हम व्यक्ति के प्रशिक्षण और चरित्र के बारे में चर्चा करते हैं तो इस चर्चा का एक पहलू तो वह है कि जिसको आजकल अरब दुनिया में ‘फ़िक़्हुल-उसरा’ के नाम से याद किया जाने लगा है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने सबसे पहले इसपर ध्यान दिया और यह बताया कि व्यक्ति के प्रशिक्षण, व्यक्ति के इस्लामी गठन और व्यक्ति की नैतिक तैयारी के लिए पवित्र क़ुरआन ने क्या-क्या निर्देश दिए हैं। इबादात, मामलात, अल-हज़्र वल-इबाहा के शीर्षक और अध्याय, जिनसे फ़िक़्ह के विद्यार्थी भली-भाँति परिचित हैं, इसी ग़रज़ को पूरा करते हैं। ‘अल-हज़्र वल-इबाहा’ के शीर्षक से इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने आम सामाजिक मामलों में जायज़ और नाजायज़ मामलों से बहस की है। यह फ़िक़्हे-इस्लामी का वह निराला विभाग है जिसको हम ‘फ़िक़्हे-तआमुले-इज्तिमाई’ कह सकते हैं। यानी सोशल इंट्रैक्शन का एक कोड। ये सभी मामलात व्यक्ति के मार्गदर्शन और व्यक्ति की कार्यकुशलता को इस्लाम के नैतिक मानदंडों से समरूप करने के लिए हैं। हलाल और हराम के ये आदेश नैतिक सिद्धान्तों पर कार्यान्वयन की कैफ़ियत को बेहतर-से-बेहतर बनाने के लिए हैं।
लेकिन व्यक्ति का नैतिक प्रशिक्षण उसके परिवार और माहौल से अलग हटकर नहीं किया जा सकता। इसलिए कि कोई व्यक्ति अकेले ज़िन्दगी नहीं गुज़ारता। आज तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने परिवार और समाज से बिलकुल कटकर आबादी के बाहर ज़िन्दगी गुज़ारी हो और ख़ुद ही नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। हर व्यक्ति का एक माहौल होता है, या तो उसका निजी और वास्तविक परिवार होता है या किसी और परिवार में वह जाकर बस जाता है। ग़रज़ किसी-न-किसी छोटे-से परिवार ही में कोई व्यक्ति प्रशिक्षण पाता है।
कुछ दार्शनिकों ने ऐसी स्थिति की कल्पना करने की कोशिश की थी कि कोई बच्चा किसी संयोग के नतीजे में माँ बाप से, बल्कि पूरी मानवजाति से बिछड़कर किसी रेगिस्तान में पहुँच जाए और जानवरों में जाकर ज़िन्दगी गुज़ारे, तो वह किस प्रकार का प्रशिक्षण पाएगा। इब्ने-तुफ़ैल एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, उसने एक दार्शनिक नॉविल लिखा था ‘हय्य-बिन-यक़ज़ान’ इस नॉविल का उर्दू अनुवाद भी ‘जीता-जागता’ के नाम से हुआ था। इब्ने-सीना ने ‘सलामान और अबसाल’ के नाम से एक फ़िक्शन नॉविल लिखा। और भी कई दार्शनिकों और मुतकल्लिमीन ने ऐसी कहानियाँ और नॉविल तैयार किए जिनमें ऐसे काल्पनिक बच्चे की ज़िन्दगी का विवरण था, जो किसी वजह से अपने माँ-बाप से बिछड़ गया और जंगल में, या किसी रेगिस्तान में, उसने जानवरों के साथ अकेले ज़िन्दगी गुज़ारी। और इस तरह वह मात्र सोच-विचार के नतीजे में सृष्टि के तथ्यों तक पहुँचा। इन नॉविलों के लेखक अपनी काल्पनिक शैली में यह दिखाना चाहते थे कि इंसान के स्वभाव और प्रकृति में भलाई की भावना मौजूद है। इंसान के स्वभाव में तौहीद (एकेश्वरवाद) की भावना मौजूद है, इंसान की प्रकृति तौहीद पर ईमान की अपेक्षा करती है। इसलिए एक ऐसा बच्चा जो पूरी ज़िन्दगी इंसानों से दूर रहा हो, जो अपने होश संभालने से पहले से लेकर सारी उम्र रेगिस्तान या जंगल में रहा हो, जिसने ज़िंदगी-भर किसी इंसान की शक्ल न देखी हो, वह कैसे उच्च आध्यात्मिक और नैतिक तथ्यों तक पहुँचता है। इसी तरह के काल्पनिक नॉविलों के अलावा कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं पाया गया जिसने इस तरह अकेले ज़िन्दगी गुज़ारकर स्वयं नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण पा लिया हो। इसलिए जब पवित्र क़ुरआन और शरीअत व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति और परिवार को एक ऐसा विषय समझकर बात करते हैं जो आपस में गहरा सम्बन्ध रखते हैं, जो आपस में एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति परिवार का गठन करता है और परिवार व्यक्ति की तैयारी में सहयोगी और सहायक होता है। दोनों एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं और एक-दूसरे के प्रशिक्षण में भाग लेते हैं।
जब परिवार की बात आती है तो मूल प्रश्न स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का पैदा होता है। इस विषय पर आगे एक चर्चा में विस्तार से बात होगी। यहाँ परिवार की बात नैतिकता के पहलू से आ गई है। स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध पवित्र क़ुरआन ने दूसरे विषयों की तुलना में कुछ विस्तार से बयान किया है। पवित्र क़ुरआन के अवतरण से पहले भी यह समस्या मौजूद थी। स्त्री-पुरुष पहले दिन से हैं। आदम और हवा एक साथ ज़मीन पर आए थे। पहले दिन से पुरुष भी मौजूद है और स्त्री भी मौजूद है। इन दो जातियों के मध्य सन्तुलन और समरसता से ही मानवता की व्यवस्था चल सकती है। लेकिन अतीत निकट में पिछले सौ डेढ़ सौ साल से पश्चिमी दुनिया ने इस समस्या को एक नया आक्रामक रंग दे दिया है, जिसके नतीजे में इन दोनों की हैसियत दो परस्पर विरोधी कैम्पों की हो गई है। दो ऐसे परस्पर विरोधी कैम्प जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ निरन्तर युद्धरत हैं और एक-दूसरे के ख़िलाफ़ अपने वास्तविक या काल्पनिक अधिकारों के बचाव के लिए हर समय लड़ते रहते हैं।
इस्लामी शरीअत का स्वभाव ग़ैर-ज़रूरी रस्साकशी और जंग का नहीं है। इस्लामी शरीअत ने पति-पत्नी को एक-दूसरे के लिए शान्ति एवं तृप्ति का साधन क़रार दिया है। एक-दूसरे के व्यक्तित्व की पूर्ति का सामान बताया है। एक को दूसरे का लिबास ठहराया है। जिस तरह लिबास इंसान के व्यक्तित्व की पूर्ति करता है, जिस तरह लिबास इंसान की बहुत-से त्रुटियों को छिपाता है, लिबास की वजह से इंसान की बहुत-सी ख़राबियाँ छिपी रहती हैं, जिस तरह इंसान की शोभा में उसके लिबास से वृद्धि होती है उसी तरह स्त्री-पुरुष यानी पति-पत्नी भी एक-दूसरे के व्यक्तित्व की पूर्ति करते हैं, एक-दूसरे की ख़राबियों की पर्दापोशी करते हैं, एक-दूसरे के व्यक्तित्व की पूर्ति और प्रशिक्षण में वृद्धि का ज़रिया बनते हैं। यह है पवित्र क़ुरआन की नज़र में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का प्रकार। इस सम्बन्ध का आधार एक-दूसरे के अधिकार को स्वीकार करने, एक-दूसरे के बारे में अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने और अदा करने पर है। स्त्री-पुरुष के बीच हर प्रकार के सम्पर्कों और सम्बन्धों का आधार नैतिकता और ‘हया’ (लाज) के सिद्धान्तों पर क़ायम है। अगर ये दो मौलिक बातें सामने रहें कि इस्लामी शरीअत ने नैतिकता और विशेषकर हया की एक धारणा दी है, इस हया की धारणा की अपेक्षा है कि इन सम्बन्धों को इस तरह संगठित किया जाए कि इन सीमाओं से बाहर कोई व्यक्ति न निकल सके और हर एक को अपने हक़ के बजाय दूसरे के हक़ की ज़्यादा फ़िक्र हो तो फिर परिवार के मामलात ख़ुशगवार और सफल रहते हैं।
व्यक्ति के प्रशिक्षण में मूल पत्थर नैतिक पराकाष्ठा और अल्लाह का डर है। इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी जितनी नैतिक धारणाएँ भी दार्शनिकों और चिन्तकों ने संकलित की हैं उनमें एक चीज़ समान है, और वह यह है कि अधिकांश चिन्तकों और दार्शनिकों ने आध्यात्मिक मूल्यों और दीनी धारणाओं से हटकर नैतिक विचारधाराएँ संकलित करने की कोशिश की। जब भी नैतिक धारणाओं को आध्यात्मिक सिद्धान्तों से हटकर संकलित करने की कोशिश की जाएगी तो वह नैतिक पराकाष्ठा की प्राप्ति में असफलता ही का सामना करेगी। ऐसी कोशिशों के नतीजे में दर्शन तो तराशे जा सकते हैं, वास्तविक नैतिकता पैदा नहीं की जा सकती। जब भी आख़िरत की जवाबदेही का एहसास दरमियान से हटा दिया जाएगा तो फिर कोई ऐसी सर्वोपरि शक्ति मौजूद नहीं रहेगी जो व्यक्ति को नैतिक पराकाष्ठा से विभूषित करने में सहायक एवं सहयोगी सिद्ध हो सके।
हिकमत (तत्त्वदर्शिता) जिसका एक मौलिक तत्त्व नैतिक पराकाष्ठा है, मुतकल्लिमीने-इस्लाम के नज़दीक बहुत-से अध्यायों पर आधारित है। व्यक्ति का प्रशिक्षण, मंज़िल पाने का जतन आदि ये सब तत्त्वदर्शिता ही के विभिन्न अध्याय हैं। इन सबका आधार अल्लाह का ख़ौफ़ और इस के सामने जवाबदेही का एहसास है। नैतिकता के महत्त्व पर मुसलमान चिन्तकों और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जो भी काम किया वह इसी मौलिक आधार को सामने रखकर किया है कि व्यक्ति में अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा किया जाए। एक बार यह एहसास पैदा हो जाए तो नैतिक पराकाष्ठा को एक-एक करके बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है। यही एहसास न केवल तक़्वा और व्यक्तिगत नैतिकता को जन्म देता है, बल्कि सामूहिकता को भी बेहतर बनाता है। इस दृष्टि से इस्लामी शरीअत के विशेषज्ञों ने आध्यात्मिकता और नैतिकता दोनों को एक ही शीर्षक के तहत बयान किया है और दोनों को एक-दूसरे की पूर्ति का ज़रिया क़रार दिया है।
पवित्र क़ुरआन में इस ग़रज़ के लिए जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है वह ‘तज़किया’ है। इस्लाम के पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कर्त्तव्यों के सन्दर्भ में पवित्र क़ुरआन में बताया गया है कि “वे इंसानों का तज़किया करते हैं”। जब दीनी और नैतिक प्रशिक्षण के नतीजे में एक इंसान का तज़किया (आन्तरिक सुधार) अन्दर से हो जाता है तो फिर उस प्रशिक्षण के नतीजे में, शरीअत का और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की भावना पैदा होती है, इसका निष्ठापूर्ण पालन करने का उत्प्रेरक दिल की गहराइयों से उठता है। इस कार्यान्वयन के नतीजे में इसके प्रभाव लोगों के परस्पर सम्बन्धों पर भी पड़ते हैं। इसके प्रभाव व्यक्ति और अल्लाह के दरमियान सम्बन्ध पर भी पड़ते हैं। इस दृष्टि से यह दो गुना प्रशिक्षण है जिसके नतीजे दो मामलों में हमारे सामने आते हैं।
मुसलमान फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन तथा इस्लामी चिन्तकों के यहाँ कभी नैतिकता और आध्यात्मिकता में किसी प्रकार के परस्पर टकराव या अन्तर्विरोध का सवाल पैदा नहीं हुआ। नैतिक पराकाष्ठा के वास्तविक आधार के बारे में इस्लामी चिन्तक कभी किसी वैचारिक या नज़रियाती उलझन का शिकार नहीं हुए। इसके विपरीत पश्चिमी दुनिया में, प्राचीन पश्चिमी दुनिया हो या आधुनिक पश्चिमी दुनिया, पूर्वी यूरोप की यूनानी सभ्यता हो, मध्य यूरोप की रोमन सभ्यता हो, या पश्चिमी यूरोप की हालिया दुनिया हो, इन सब में मौलिक सवाल जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है वह नैतिकता के बौद्धिक एवं वैचारिक आधार का रहा है। नैतिकता को किस आधार पर क़ायम किया जाए, इसपर पश्चिमी दुनिया में कभी मतैक्य नहीं हो सका। यूनानियों ने इसका समाधान यह निकाला कि दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों और रवैयों के दरमियान सन्तुलन का नाम नैतिकता है। बौद्धिक दृष्टि से यह एक अच्छी बात मालूम होती है। इसपर अच्छी किताबें लिखी जा सकती हैं। लेख लिखे जा सकते हैं, लेकिन ख़ुद इस सन्तुलन का निर्धारण कैसे किया जाएगा? और किस आधार पर किया जाएगा, इसका कोई निर्धारित वास्तविक, बौद्धिक और निश्चित आधार यूनानियों के पास भी मौजूद नहीं है।
यूनानी चिन्तकों का कहना था कि हर इंसान के अन्दर एक ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ (क्रोध-शक्ति) होती है जो हर अप्रिय चीज़ के ख़िलाफ़ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अप्रिय या स्वभाव के विपरीत बात पर हर इंसान क्रोधित होता है। अव्वल तो यही बात वास्तविकता के ख़िलाफ़ है कि हर इंसान क्रोधित होता है। बहुत-से इंसान क्रोधित नहीं होते। बहुत-से लोगों को हम देखते हैं जिनको ग़ुस्सा नहीं आता। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हर इंसान में ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ समान रूप से मौजूद होती है तो यूनान के लोगों का तर्क यह था, इस ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ के सन्तुलन का नाम नैतिकता है। इस शक्ति का एक आरम्भ है, और एक चरम। अगर यह शक्ति हद से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा करना शिष्टाचार और नैतिकता के ख़िलाफ़ है और अगर वह हद से गिर जाए तो कायरता, निर्लज्जता और आत्मसम्मानहीनता है। यह चीज़ भी नैतिकता के ख़िलाफ़ है। अत: इन दोनों इंतिहाओं के दरमियान सन्तुलन होना चाहिए। लेकिन वह सन्तुलन कहाँ क़ायम हो, वह काँटा तराज़ू इस बिन्दु पर या उस बिन्दु पर हो, उसका कोई आधार मौजूद नहीं है।
चुनाँचे पश्चिमी दुनिया में जितने नैतिकता के उपदेशक रहे हैं, या नैतिकता पर कार्यान्वयन होने के दावेदार रहे हैं उनमें से हर व्यक्ति ने अपनी पसन्द-ना-पसन्द के आधार पर, अपने निजी, वर्गीय या भाषागत हितों के आधार पर इस सन्तुलन-बिन्दु का निर्धारण किया। आज भी जो ताक़तवर है वह अपने हितों में सन्तुलन-बिन्दु का निर्धारण करता है, जो कमज़ोर है वह अपने अन्दाज़ से निर्धारण करने की कोशिश करता है। जिसका अपना हित चर्चा का विषय है वह अपने हितों की रौशनी में सन्तुलन-बिन्दु का निर्धारण करता है। सन्तुलन-बिन्दु की कोई सारगर्भित परिभाषा न तो यूनानियों के यहाँ पाई जाती थी और न आधुनिक काल के पश्चिम में पाई जाती है। इसका हल कुछ लोगों ने यह निकाला कि उपयोगिता को आधार क़रार दिया, यानी जो चीज़ इंसानों के लिए लाभकारी है वह नैतिक है और जो इंसानों के लिए अलाभकारी है वह अनैतिक है। इसके बाद पश्चिमी चिन्तकों ने कहना शुरू किया कि अस्ल मापदंड उपयोगिता नहीं, बल्कि निजी पसन्द है। जो चीज़ इंसान को पसन्द है वह नैतिक है और जो ना-पसन्द वह अनैतिक। इससे भी आगे बढ़कर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो मौजूद है वह वास्तविक है और वही नैतिकता का आधार है, जो मौजूद नहीं है वह अवास्तविक है, उसपर नैतिकता की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। इस तरह की बहस से विचारधाराएँ और धारणाएँ तो बहुत पैदा हो गईं। विचारधाराओं का फैलाव (proliferation) तो बहुत हो गया लेकिन वास्तविक नैतिकता की निशानदेही न अतीत में हो सकी, न आज हो सकी है।
पवित्र क़ुरआन ने इस तरह के किसी अवास्तविक आधार, मात्र विचारधाराओं और विशुद्ध बौद्धिक धारणाओं पर ज़ोर देने के बजाय इंसान के व्यक्तिगत प्रशिक्षण और ‘फ़ितरते-सलीमा’ (अच्छा स्वभाव) को सामने रखा है, पवित्र क़ुरआन ने बताया है कि हर इंसान में एक ‘फ़ितरते-सलीमा’ रख दी गई है। हर इंसान के अन्दर एक ऐसी प्रकृति मौजूद है जो ख़ुद-ब-ख़ुद भलाई की माँग करती है और बुराई से नफ़रत करती है। यही वजह है कि हर इंसान अपने मूल और अस्तित्व से अच्छा इंसान होता है और आम नैतिक सिद्धान्तों से विमुख नहीं होता। बाहरी शक्तियों के प्रभाव से उसमें भटकाव पैदा होता है। समाजों में मौजूद नकारात्मक प्रवृत्तियाँ उसकी ‘फ़ितरते-सलीमा’ में बिगाड़ पैदा करती हैं। यह ‘फ़ितरते-सलीमा’ अगर प्रशिक्षण के नतीजे में और पक्की और मुकम्मल हो जाए और उसमें बुराई के ख़िलाफ़ प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाए तो फिर तमाम नैतिक समस्याएँ सुविधापूर्वक ख़ुद-ब-ख़ुद हल होते चले जाते हैं और व्यक्ति की सामाजिक और नैतिक मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं।
जिन लोगों ने इंसानों के प्रशिक्षण को इस दृष्टिकोण से देखा कि उनको अच्छे शिष्ट इंसान कैसे बनाया जाए, शरीअत के नैतिकता के मापदंड और पूर्णता के मापदंड की रौशनी में उनको परिपूर्ण इंसान कैसे बनाया जाए। उन्होंने नैतिकता, आध्यात्मिकता के साथ-साथ शरीअत के आदेशों को भी सामने रखा और इंसान के नैतिक प्रशिक्षण और आध्यात्मिक सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम संकलित करने की कोशिश की। ऐसे विद्वानों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उनमें कुछ व्यक्तित्व बहुत नुमायाँ हैं जिनके विचार और धारणाएँ और जिनके ज्ञानपरक काम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त हुई।
उनमें एक बहुत नुमायाँ नाम हुज्जतुल-इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली (रह॰) का है जिनके विचारों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। हमारे उपमहाद्वीप के इस्लामी चिन्तक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) का नाम भी इस मैदान में बहुत नुमायाँ है। उन लोगों ने जो लिखा है वह उन्होंने इसी क्रम से बयान किया है। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। अगरचे बात आम है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन इस अन्दाज़ से जब कही जाए तो इसमें एक नई सार्थकता पैदा होती है। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने इंसान के बारे में लिखा है कि अगरचे वे अज़ल (अनादिकाल) से नहीं लेकिन अब्दी (शाश्वत) ज़रूर है, ज़ाहिर है कि इंसान अज़ल से नहीं है। एक ज़माना था कि इंसान मौजूद नहीं था। क़ुरआन भी यही बताता है— “बेशक इंसान पर एक ऐसा भी समय बीता है, जब वह कोई उल्लेखनीय चीज़ न था।” (क़ुरआन, 76:1) लेकिन वह अबदी ज़रूर है। एक बार अल्लाह ने पैदा कर दिया तो इस उद्देश्य के लिए पैदा किया कि अब वह हमेशा रहेगा। अबदियत (शाश्वत होने का गुण) इंसान को प्राप्त है। अज़लियत (अनादिकाल से होने का गुण) प्राप्त नहीं। इससे इमाम ग़ज़ाली नए-नए बिन्दु निकालते हैं।
एक बिन्दु इस बात से उन्होंने यह निकाला कि इसका मतलब यह है कि इंसान में एक तरफ़ एक साथ माद्दियत (भौतिकता) भी पाई जाती है और दूसरी तरफ़ मलकूतियत (फ़रिश्तोंवाला गुण) भी पाई जाती है। आंशिक रूप से माद्दियत पाई जाती है, आंशिक रूप से ही मलकूतियत भी पाई जाती है। इंसान के मुक़ाबले में फ़रिश्ते बहुत लम्बे समय से हैं, बहुत लम्बे समय से चले आ रहे हैं। और एक लम्बे समय तक अल्लाह ने उनको ज़िन्दगी दी है। यह फ़िरश्तों की ज़िन्दगी का वह पहलू है जो इंसान को एक तरफ़ से दिया गया है। अबदियत के पहलू से दिया गया, इंसान को अज़लियत प्राप्त नहीं है। इंसान हादिस (अस्तित्व में आनेवाला) है। बाद में उसका अस्तित्व सामने आता है। इसलिए कि उसमें माद्दियत के सख़्त तत्त्व नुमायाँ तौर पर पाए जाते हैं। इस बात को इमाम ग़ज़ाली इस अन्दाज़ से कहते हैं कि अगरचे इंसान का शारीरिक अस्तित्व और इंसान का जिस्म ख़ाकी और सिफ़ली (घटिया) है, लेकिन उसकी रूह की वास्तविकता और प्रवृत्तियाँ उलवी (उच्चकोटि की) और रब्बानी हैं। उसमें रब की शान भी पाई जाती है और उलवियत (उच्च होने का गुण) भी पाई जाती है। इसलिए इसमें पाशविक और हैवानी गुणों के साथ-साथ, अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों के गुण भी रखे हैं। अब उसके प्रशिक्षण का लक्ष्य यह है कि इंसान के अन्दर जो पाशविकता का तत्त्व है वह मलकूतियत के कंट्रोल में आ जाए, दूसरे शब्दों में इंसान के पाशविक और हैवानी गुण फ़रिश्तों के गुणों के अधीन हो जाएँ। पाशविकता को समाप्त करना शरीअत का अभीष्ट नहीं है।
पवित्र क़ुरआन ने कहीं यह नहीं कहा कि इंसानों में मौजूद पाशविक विशिष्टताएँ और उनकी पाशविकता समाप्त हो जानी चाहिए। न शरीअत इस काम के लिए आई है कि इंसान की विशुद्ध शारीरिक माँगों और भौतिक प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त कर दे। इसलिए कि अगर पाशविकता बिलकुल समाप्त हो जाए और मानव जीवन में केवल आध्यात्मिक पहलू ही बाक़ी रह जाए तो इंसान फ़रिश्तों की पंक्ति में शामिल हो जाएगा और आदम के नाम से और अधिक फ़रिश्ते पैदा करना अल्लाह तआला का उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य तो ऐसा प्राणी पैदा करना था कि जो बिगाड़ और फ़साद भी फैला सके, ख़ून भी बहा सके और इसके साथ-साथ अल्लाह की पाकी भी बयान कर सके। आदम की सन्तान में इन दोनों कामों की क्षमता और प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं। अत: अगर इंसान के पाशविक पहलू को निकाल दिया जाए तो यह अल्लाह तआला की उस निश्चित नीति के ख़िलाफ़ है जिसके अनुसार इंसान को पैदा किया गया था, लेकिन जब इंसान अपनी इन फ़रिश्तों जैसी विशिष्टताओं को ख़ुद नज़रअन्दाज़ कर देता है और केवल पाशविकता के पंजे में गिरफ़्तार हो जाता है तो वह ‘सब नीचों से नीच’ का दर्जा कहलाता है, जिसमें उसकी हैसियत पाशविकता से भी बदतर हो जाती है। पवित्र क़ुरआन में एक जगह यही बात कही गई है कि “ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि चौपायों से भी बदतर और ज़्यादा गुमराह हैं।” (क़ुरआन, 7:179) यह कोई अपशब्द कहना नहीं है। अल्लाह तआला को किसी को अपशब्द कहने की ज़रूरत नहीं। यह एक वास्तविकता का इज़हार है कि इंसान दो गुणों से विभूषित था। एक फ़रिश्तों का गुण था, एक पशुओं का गुण था। फ़रिश्तों का गुण समाप्त कर दिया जाए तो पशुओं ही का गुण रह जाएगा। यह हैवान जिसने ख़ुद जान-बूझकर अपने फ़रिश्तोंवाले गुणों को प्रभावित किया, फ़रिश्तोंवाले गुणों को नष्ट किया, वह निश्चय ही उस पशु से बदतर ही होगा, जिसको सिरे से मलकूतियत प्राप्त ही नहीं थी। इसलिए यह एक बड़ी वास्तविकता का इज़हार है। यह कोई अपशब्द कहना नहीं है।
मैंने इससे पहले बताया था कि हर इंसान के अन्दर इस पाशविक भावना की वजह से हमेशा मन की इच्छाएँ मौजूद रहती हैं। इन मन की इच्छाओं को ख़त्म करना शरीअत का मंशा नहीं है, बल्कि शरीअत का मंशा उन मन की इच्छाओं की हदबन्दी करना है। शरीअत की तमाम ज़िम्मेदारियों का अभीष्ट यही है, दूसरे शब्दों में शरीअत के तमाम आदेशों और शरीअत की तरफ़ से डाली गई तमाम पाबन्दियों की अस्ल ग़रज़ यह है कि इंसान की मन की इच्छाओं में अनुशासन आ जाए और उनको सीमाओं का पाबन्द कर दिया जाए। इस विषय को लगभग तमाम इस्लामी चिन्तकों, क़ुरआन के टीकाकारों, सूफ़ियों और दूसरे बहुत-से विद्वानों ने बयान किया है। कुछ लोगों ने इसलिए ‘ज़ब्ते-नफ़्स’ (इच्छाओं पर नियंत्रण) का शीर्षक प्रयोग किया है। अल्लामा इक़बाल ने ‘ख़ुदी’ की शब्दावली प्रयुक्त की है। उनके यहाँ ‘ज़ब्ते-नफ़्स’ की शब्दावली भी मिलती है। ‘बे-ख़ुदी’ की शब्दावली भी मिलती है। ‘ज़ब्ते-नफ़्स’ की सर्वप्रथम पहचान यह है कि इंसान की इच्छाएँ उसके कंट्रोल में हों और भौतिक और शारीरिक इच्छाएँ उसकी उत्प्रेरक भावना के अधीन और वास्तविक आधार न हों। मन को अपना रब बना लेने की कैफ़ियत न हो, बल्कि कैफ़ियत यह हो कि “जिसने इस भावना को पवित्र बनाया वह सफल हुआ और जिसने इस भावना को और ख़राब किया वह असफल रहा।” (क़ुरआन, 91:9-10)
नैतिक प्रशिक्षण की जब भी बात हुई है तो एक सवाल हमेशा नैतिकता के दार्शनिकों के सामने रहा है कि नैतिक प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? मुसलमान की नज़र में मूल उद्देश्य का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए कि जहाँ यह ईमान हो कि यह ज़िन्दगी अस्थायी है और आख़िरकार एक नई ज़िन्दगी आनी है जहाँ सफलता और असफलता के परिणाम सामने आएँगे वहाँ मंज़िले-मक़्सूद का सवाल निश्चित है और स्पष्ट है। लेकिन जिन क़ौमों में आख़िरत या परलोक की कोई धारणा नहीं है, या बहुत कमज़ोर है, उनके यहाँ यह सवाल मौलिक महत्त्व रखता है कि नैतिक प्रशिक्षण क्यों किया जाए? इस प्रशिक्षण का उत्प्रेरक क्या है और इसके नतीजे में क्या प्राप्त करना अभीष्ट है।
यूनानियों ने इसके लिए जो शब्दावली प्रयुक्त की है उसका अंग्रेज़ी अनुवाद happiness यानी ख़ुशी है। मालूम नहीं कि इस सन्दर्भ में अस्ल यूनानी शब्द क्या है और इसका वास्तविक अनुवाद क्या है? लेकिन हकीम अरस्तातालीस और दूसरे यूनानी चिन्तकों ने जो शब्दावली प्रयुक्त की उसका अनुवाद पश्चिमी लेखकों ने ‘ख़ुशी’ और ‘प्रसन्नता’ के अंग्रेज़ी पर्यायवाची शब्द के द्वारा किया है, यों उन्होंने happiness यानी ख़ुशी और प्रसन्नता को मानव जीवन का आख़िरी और वास्तविक गन्तव्य ठहराया है। उनके ख़याल में हर इंसान ख़ुशी और प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ख़ुद प्रसन्नता क्या है? इसपर जब यूनानियों ने ग़ौर किया तो उनमें से बहुत-से लोगों ने यह महसूस किया कि जब इंसान को आनन्द प्राप्त होता है तभी उसको प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। स्वादिष्ट खाने खाता है तो ख़ुश होता है। अच्छा लिबास पहनता है तो ख़ुश होता है। इसी तरह दूसरी बहुत-से स्वाद और आनन्द, शारीरिक और भौतिक आनन्द, ऐसी हैं कि जब वे प्राप्त होते हैं तो इंसान ख़ुश होता है। अत: आनन्द और प्रसन्नता दोनों एक-दूसरे के पूरक क़रार पा गए। अगर मज़े ही की प्राप्ति को इंसान के सारे प्रयासों का लक्ष्य क़रार दे दिया जाए तो इससे जो नैतिक ख़राबियाँ और तबाहियाँ पैदा होती हैं उनका अन्दाज़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है।
शायद इसी लिए मुतकल्लिमीने-इस्लाम और सूफ़ियों ने विशेष रूप से, और मुस्लिम दार्शनिकों ने आम तौर से इसके लिए ‘सआदत’ की शब्दावली प्रयोग की है। ‘सआदत’ का शब्द पवित्र क़ुरआन में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। पवित्र क़ुरआन ने सफल इंसान को ‘सईद’ क़रार दिया है। पवित्र क़ुरआन की नज़र में इंसान दो प्रकार के हैं। एक प्रकार उन इंसानों का है जिनको ‘सआदत’ और सौभाग्य प्राप्त है। दूसरे वे हैं जिनको सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वे अभागे हैं। ‘सआदत’ के शब्द में वे तमाम खूबियाँ शामिल हैं जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल का लक्ष्य हैं और जो इंसान को इस दुनिया में और आख़िरत में सफलता दिला सकती हैं। वास्तविक ‘सआदत’ की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि वे उपाय अपनाए जाएँ जो इंसान को पाशविकता के नकारात्मक परिणामों से सुरक्षित रखें, मानवता के मलकूती पहलू को बढ़ाएँ और इस दुनिया में सुधार और आख़िरत में सफलता के लिए इंसानों को सफल और हक़दार बनाएँ।
हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ‘सआदत’ की वास्तविकता पर चर्चा करते हुए लिखा है कि ‘सआदत’ और इंसानी कमालात (पराकाष्ठाओं) के दो दर्जे हैं। कमाल (पराकाष्ठा) का एक दर्जा तो वह है जो ख़ुद मानवता की माँग है और हर इंसान को इंसान होने की हैसियत में इस दर्जे को प्राप्त करना चाहिए। दूसरा दर्जा वह है जिसमें इंसान दूसरी सांसारिक रचनाओं के साथ शामिल है। इन दोनों दर्जों में अस्ल दर्जा पहला ही है। जिसको हर समझदार और सद्बुद्धि रखनेवाला इंसान प्राप्त करना चाहता है।
जहाँ तक कमाल के दूसरे दर्जे का सम्बन्ध है तो वह इन गुणों पर आधारित है जो जड़ वस्तुओं, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों को भी प्राप्त होते हैं, उदाहरणार्थ कुछ लोग शारीरिक क़द-काठी पर बहुत ज़ोर देते हैं और यह याद नहीं रखते कि अगर ऊँचा क़द और मज़बूत जिस्म ही कमाल की अस्ल बुनियाद होता तो पहाड़ सबसे ज़्यादा बा-कमाल कहलाने के हक़दार थे। बहुत-से लोग ज़ाहिरी ख़ूबसूरती और सौन्दर्य ही को अस्ल कमाल समझते हैं। अगर ज़ाहिरी सौन्दर्य ही अस्ल कमाल होता तो ख़ूबसूरत पौधे, बाग़-बग़ीचे और वनस्पतियाँ ही बा-कमाल कहला सकतीं। कुछ और लोगों की नज़र में कमाल यह है कि इंसान की शारीरिक शक्ति बहुत हो, वह लैंगिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो, बहुत खाता-पीता हो, भूख ख़ूब खुली हुई हो। अगर यही सब कुछ पराकाष्ठा का मापदंड और ‘सआदत’ की शर्त है तो घोड़े, गधे, ख़च्चर और चौपाए, बल्कि दरिंदे सबसे ज़्यादा बा-कमाल और सईद तथा भाग्यवान क़रार पाते।
सआदत, सौभाग्य और कमाल का अस्ल पैमाना नैतिक पराकाष्ठा, मन की शिष्टता, सामाजिक तथा सांसकृतिक, विभिन्न कलात्मक निपुणताएँ और इंसान का सौभाग्य है। यही वजह है कि दुनिया की हर सभ्य क़ौम और तमाम सद्बुद्धि रखनेवाले और बुद्धिमान इंसान इन्हीं मापदंडों को प्राप्त करना चाहते हैं। अत: साबित हुआ कि अस्ल कमाल और सौभाग्य यह है कि इंसान की विशुद्ध भौतिक, शारीरिक और पाशविक माँगें उसकी बुद्धि और अन्तर्दृष्टि के अधीन हों, उच्च नैतिकता और सभ्यता की प्राप्ति का यही एकमात्र रास्ता है।
नैतिक पराकाष्ठा की प्राप्ति और सभ्यता मनेच्छा की पूर्ति बहुत मेहनत और लम्बा अभ्यास चाहती है। इस मेहनत और अभ्यास के बिना प्रबल भौतिक प्रवृत्तियाँ और मुँह-ज़ोर पाशविक माँगों पर क़ाबू पाना सम्भव नहीं। इसलिए कि ख़ुद उन प्रवृत्तियों और माँगों की शक्ति और मुँह ज़ोरी से परे वातावरण में चारों ओर वे शक्तियाँ दिन-रात कार्यरत रहती हैं जो इन माँगों को और मुँहज़ोर बनाती हैं, और उन प्रवृत्तियों की शक्ति में और अधिक वृद्धि करती रहती हैं। इसलिए एकाग्र होकर लगातार मेहनत और अभ्यास के बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं होता।
शरीअत ने जिन इबादतों का आदेश दिया है वे इंसान को इस रास्ते पर लाने में बहुत प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। शाह साहब ने अपनी बहुमूल्य किताब ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ में यही साबित किया है कि इबादतों और शरीअत के आदेशों की इंसान की ‘सआदत’ की प्राप्ति में क्या भूमिका है। उन्होंने शरीअत के एक-एक आदेश पर अलग-अलग बहस करके बताया है कि इससे इंसान की सआदत, सौभाग्य और कमाल की कौन-कौन-सी माँगें पूरी होती हैं।
यह सारांश है इस अर्थ का जो ‘सआदत’ के बारे में बड़े-बड़े इस्लामी चिन्तकों, इमाम ग़ज़ाली, फ़ाराबी, इब्ने-सीना और बहुत-से इस्लामी विद्वानों ने बयान किया है। इन लोगों के लेखों में अन्तर केवल विस्तृत विवरण और सारांश और शब्दावलियों और वर्णन शैली का है। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) और शाह वलीउल्लाह (रह॰) दोनों ने लिखा है कि ‘सआदत’ की प्राप्ति के सन्दर्भ में इंसानों के आम तौर से चार दर्जे होते हैं। और देखा यह गया है कि हर दौर में यह चारों वर्ग ‘सआदत’ के हवाले से मौजूद रहते हैं। शाह साहब की राय में कुछ लोग तो वे होते हैं कि जिनको न ‘सआदत’ प्राप्त होती है और न उम्मीद है कि उनको कभी ‘सआदत’ प्राप्त होगी। यानी उन्होंने अपनी पाशविकता को इतना प्रबल और अजेय बना दिया है कि अब उनमें फ़रिश्तोंवाले तत्त्व या तो बिलकुल समाप्त हो गए हैं या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उनको दोबारा सक्रिय और प्रभावकारी बनाना सम्भव नहीं रहा।
यह वह वर्ग है जिसके बारे में पवित्र क़ुरआन में कहा गया है “ये अंधे भी हैं, गूँगे भी और बहरे भी, इसलिए ये किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रखते।” (क़ुरआन, 2:171) दूसरा वर्ग वह होता है कि जो काफ़ी बड़ी संख्या में होता है जिसको फ़िलहाल तो ‘सआदत’ प्राप्त नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ‘सआदत’ प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कि उसके अन्दर की पाशविकता अभी पूरे तौर पर प्रभावी नहीं हुई, और मलकूतियत भी पूरे तौर पर समाप्त नहीं हुई। शाह वलीउल्लाह (रह॰) कहते हैं कि इंसानी समाजों में अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की होती है। पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) को भेजे जाने का अस्ल उद्देश्य ऐसे ही लोगों का सुधार होता है। इतिहास से भी यही पता चलता है कि पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) का साथ देनेवालों में अधिक संख्या का सम्बन्ध इसी वर्ग से रहा है।
इस वर्ग के कंकड़-पत्थर समान साधारण लोग पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) के प्रशिक्षण से हीरे-मोती बन-बनकर निकले। एक तीसरा वर्ग जो संख्या में तुलनात्मक रूप से कम होता है उन लोगों पर सम्मिलित होता है जो जन्मजात रूप से, अपनी प्रकृति की दृष्टि से, अपने स्वभाव और प्रशिक्षण की दृष्टि से ऐसे होते हैं कि उन्होंने ख़ुद अपने अन्दर की मलकूती प्रवृत्तियों और तत्त्वों को विकास दे रखा होता है और अपने अन्दर की पाशविकता को कंट्रोल किया हुआ होता है। ये वे लोग हैं जो हर ज़माने में भलाई के हर काम में ‘साबिक़ीन अव्वलीन’ (सबसे पहले आगे बढ़नेवाले) होते हैं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में बहुत-से ऐसे सीधे-सादे और भाग्यवानों की मिसालें मिलती हैं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसे ही चरित्रवान लोगों के बारे में फ़रमाया था कि “जो जाहिलियत में अच्छे और सईद थे, वे इस्लाम में भी अच्छे और सईद हैं, भाग्यवान हैं।”
बहुत सीमित संख्या में एक वर्ग वह होता है जिसमें न केवल फ़िलहाल ‘सआदत’ मौजूद होती है, बल्कि और अधिक ‘सआदत’ की असाधारण प्रतिभाएँ भी मौजूद होती हैं, बल्कि अल्लाह तआला ने इस वर्ग को यह क्षमता और हिम्मत दी है कि वह दूसरों को भी ‘सआदत’ और ख़ैर की तरफ़ ला सकता है। ये वे लोग हैं जिनको पवित्र क़ुरआन में ‘वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून’ कहा गया है। ये ख़ुशनसीब लोग ‘साबिक़ीन अव्वलीन’ में भी सबसे पहले आगे बढ़नेवाले लोग हैं। “और आगे बढ़ जानेवाले तो आगे बढ़ जानेवाले ही हैं। वही (अल्लाह के) निकटवर्ती हैं।” (क़ुरआन, 56:10-11) जो हर दौर और हर ज़माने में इंसानों के लिए मार्गदर्शन का ज़रिया बनते हैं। और इंसानियत के लिए मान-सम्मान का कारण होते हैं। बड़े प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का सम्बन्ध इसी वर्ग से था।
यह बात उल्लेखनीय है कि ऐसे ही या इससे मिलते-जुलते चार वर्ग इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने भी गिनवाए हैं। शाह साहब के विपरीत उन्होंने ज़्यादा ध्यान इस अभागे वर्ग पर रखा है जिसको ‘सआदत’ प्राप्त नहीं है। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) के विभाजन के अनुसार नैतिक प्रशिक्षण से दूरी और नैतिक पराकाष्ठा से वंचित होने के मामले में इंसानों के निम्नलिखित चार दर्जे हैं।
- जाहिल या नादान
- जाहिल गुमराह
- जाहिल गुमराह बदकार
- जाहिल गुमराह बदकार बदकिरदार
सबसे पहला यानी जाहिल या नादान से मुराद वह नादान ग़फ़लत में पड़ा इंसान है जो न सत्य-असत्य में भेद कर सकता है और न अच्छे-बुरे में फ़र्क़ कर सकता है। उसका ज़ेहन सादा और स्वाभाविक ढंग पर क़ायम है, न उसमें किसी अच्छे अक़ीदे का असर है, न किसी ग़लत अक़ीदे का वह समर्थक है। न उसको अच्छे विचारों और सत्कर्मों का ज्ञान है और न लज़्ज़तों और मन की इच्छाओं की पैरवी ने उसके दिल-दिमाग़ को निष्क्रय किया है। ऐसा व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने की पूरी तरह क्षमता रखता है, उसको केवल एक अच्छे शिक्षक या प्रशिक्षक की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द उच्च नैतिकता से विभूषित हो सकता है।
दूसरा वर्ग वह है जो बुरे को बुरा तो समझता है, ग़लत को ग़लत मानता भी है, लेकिन उसको सत्कर्म करने की इच्छा नहीं हुई, वह अपनी इच्छाओं और व्यर्थ के कामों में इतना लीन है कि उनको अच्छा समझने लगता है। आनन्दप्रिय होने की वजह से अच्छाई को अच्छाई मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी सुधार योग्य है, लेकिन उसके सुधार के लिए बहुत मेहनत और लम्बे समय तक प्रशिक्षण दरकार है। ऐसा व्यक्ति अगर हिम्मत से काम ले तो उसका प्रशिक्षण हो सकता है।
रहा तीसरा वर्ग सो वह उन अभागे लोगों पर सम्मिलित है जो बुरे को अच्छा और दुर्भाग्य को सौभाग्य समझते हैं। उनकी उठान ही ग़लत को सही मानने पर होती है। इस वर्ग का सुधार कभी-कभार ही हो पाता है, लेकिन बहरहाल हो सकता है और हो भी जाता है। जहाँ तक चौथे वर्ग का सम्बन्ध है तो वह न केवल बुराई को भलाई, और शर को ख़ैर समझता है, बल्कि उसकी ओर दूसरों को बुलाता भी है। यही वर्ग ख़ैर और भलाई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। इस वर्ग का सुधार भेड़ियों को सधाने के समान है।
शाह वलीउल्लाह के नज़दीक जब इंसान इस ‘सआदत’ की प्राप्ति के लिए पहल करता है तो उसको दो प्रकार के काम करने होते हैं। कुछ काम तो वे हैं जो कि ज़ाहिरी दृष्टि से इसलिए करने चाहिएँ कि इंसान अपने ज़ाहिर को वास्तविक ‘सआदत’ की माँगों के अनुसार ढाल सके। शाह वलीउल्लाह (रह॰) के शब्द हैं कि “इंसान अपने ज़ाहिर को ‘सआदत’ के तक़ाज़ों के अनुसार ढाल सकें।” शाह साहब ने लिखा है कि शरीअत ने जितने आदेश दिए हैं, जो-जो इबादतें मुक़र्रर की हैं, मामलात के बारे में जो-जो निर्देश दिए हैं। यह सब-का-सब इसी लिए है कि इंसान का ज़ाहिर उसकी वास्तविक ‘सआदत’ के तक़ाज़ों से मेल खाए। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसका सम्बन्ध अन्दर के सुधार से होता है। बज़ाहिर वह सुधार नज़र नहीं आता, बज़ाहिर इंसान की ज़ाहिरी हालत पर उसका ज़्यादा असर महसूस नहीं होता। लेकिन इस सुधार के नतीजे में इंसान के अन्दर अल्लाह से डरने की एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि इंसान एक ख़ास अन्दाज़ में ख़ुद-ब-ख़ुद बेहतरी की तरफ़ सफ़र करने लगता है। धीरे-धीरे शरीअत उसके लिए उसका स्वभाव बन जाती है। शरीअत पर वे कार्यन्वयन इस तरह करने लगता है कि “जिस तरह हदीस में है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, इसलिए कि अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे तो यह यक़ीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है।”
जब वास्तविक ‘सआदत’ की यह मंज़िल प्राप्त हो जाती है तो उसके चार संकेत सामने आते हैं।
1. पहला नतीजा तो यह होता है कि इंसान के अन्दर जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, जिसके लिए शाह के लेखों में ‘बहीमियत’ (पाशविकता) की शब्दावली बहुत अधिक प्रयोग की गई है। वे प्रवृत्तियों इंसान की सकारात्मक नैतिक और इंसानी प्रवृत्तियों के अधीन हो जाती हैं।
2. जब ऐसा हो जाए तो फिर इंसान की सारी भौतिक और शारीरिक इच्छाएँ इंसान की बुद्धि के अधीन हो जाती हैं। बुद्धि इच्छाओं के अधीन नहीं होती, बल्कि इच्छाएँ बुद्धि के अधीन हो जाती हैं।
3. तीसरा नतीजा यह निकलता है कि इंसान की वाक्-शक्ति उसकी पाशविक शक्तियों पर पूरे तौर पर हावी हो जाती है, गोया इंसान की वास्तविकता, अन्दर से ख़ुद-ब-ख़ुद इस प्रक्रिया के नतीजे में शरीअत के आदेशों और अक़ीदों के अनुरूप हो जाती है। फिर उसके लिए शरीअत ख़ुद उसका स्वभाव बन जाती है। दूसरे इंसान जिसपर मुश्किल से अमल करते हैं, वह एक प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक बात हो जाती है और उससे ख़ुद-ब-ख़ुद शरीअत के आदेशों पर कार्यान्वयन होना शुरू हो जाता है।
4. और आख़िरी चीज़ यह कि उसकी सद्बुद्धि को उसकी मनेच्छाओं पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, दूसरे शब्दों में उसको ‘हुज़ूरी’ (अल्लाह द्वारा हर समय देखे जाने) की वह कैफ़ियत प्राप्त हो जाती है, जिसको हदीस में ‘एहसान’ के शब्द से याद किया गया है।
इमाम ग़ज़ाली और शाह वलीउल्लाह वग़ैरा ने लिखा है कि इस कैफ़ियत को प्राप्त करने के लिए दो तरह के उपाय अपनाने पड़ते हैं। कुछ उपाय तो वे हैं जो ज्ञानपरक उपाय कहलाते हैं, कुछ उपाय व्यावहारिक उपाय हैं। ज्ञानपरक उपायों में सांसारिक ज्ञान भी शामिल है और शरीअत का ज्ञान भी। सांसारिक उपायों में प्रशिक्षण भी शामिल है और ज़ाहिरी तौर पर इंसान के मन को सभ्य बनाना भी। ये सब ज्ञानपरक उपाय हैं। व्यावहारिक उपाय से मुराद इंसान को एक ऐसे समाज का उपलब्ध होना और एक ऐसे माहौल का उपलब्ध होना है जहाँ उसके लिए इन चीज़ों पर अमल करना आसान हो जाए।
अब चूँकि ज्ञान का मौलिक महत्त्व यह है कि इसके बिना प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो सकता। प्रशिक्षण के बिना व्यक्ति उच्चस्तरीय व्यक्ति नहीं बन सकता। आदर्श व्यक्ति के बिना आदर्श परिवार अस्तित्व में नहीं आ सकता। आदर्श परिवार के बिना आदर्श ‘उम्मत’ अस्तित्व में नहीं आ सकती। ‘उम्मत’ के बिना इंसानियत का सुधार नहीं हो सकता। ‘उम्मत’ के बिना राज्य क़ायम नहीं हो सकता। राज्य की सहायता और संसाधन के बिना शरीअत के बहुत-से आदेशों का पालन नहीं हो सकता। इसलिए मूल सिद्धान्त मौलिक रूप से ज्ञान ठहरता है। अब ज्ञान भी एक इकाई है। दीनी ज्ञान हो या सांसारिक ज्ञान, दोनों एक ही बड़ी वास्तविकता की विभिन्न निशानियाँ हैं। वास्तविकता एक है। बड़ी वास्तविकता एक है। इसलिए जिस ज्ञान का सम्बन्ध इस बड़ी वास्तविकता से जितना क़रीबी है वह ज्ञान उतना अनिवार्य है। जितना दूर है उतना ही अनिवार्य नहीं है।
एक मरहला ऐसा आता है कि ज्ञान की हैसियत फ़र्ज़े-ऐन की होती है। इसके बाद एक मरहला ऐसा आता है कि ज्ञान की हैसियत फ़र्ज़े-किफ़ाया की होती है। उसके बाद एक दर्जा होता है कि ज्ञान की कैफ़ियत मात्र एक ऐसे बिन्दु की होती है जिसको उपमहाद्वीप के कुछ विद्वानों ने ज्ञान के दस्तरख़ान की चटनी से उपमा दी है। दस्तरख़ान पर चटनियाँ भी होती हैं, लेकिन वे main course का हिस्सा नहीं होतीं, और हो भी नहीं सकतीं, लेकिन चटनी के बिना दस्तरख़ान पूर्ण भी नहीं हो सकता, इसी तरह से ज्ञान का एक दर्जा है जिसको इमाम शातबी (रह॰) ने ‘मिलहुल-इल्म’ के नाम से याद किया है। वे कहते हैं कि एक तो ज्ञान का मूल यानी core होता है, और दूसरा हिस्सा वह होता है कि जो ज्ञान का core तो नहीं है लेकिन उसकी सीमाओं पर है और एक वह है जो ‘मिलहुल-इल्म’ की हैसियत रखता है। इसके अलावा जो कुछ है उसका ज्ञान से सम्बन्ध नहीं है और वह लाभ रहित ज्ञान है। यह तर्क उन्होंने उस हदीस से किया जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “ऐ अल्लाह! मैं लाभ रहित ज्ञान से तेरी पनाह माँगता हूँ।” इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान का एक दर्जा या एक सतह ऐसी हो सकती है कि वह लाभ रहित हो, उसको ज्ञान कहा जा सकता है और वह वास्तविकता से किसी-न-किसी हद तक सम्बन्ध भी रखता है। लेकिन इसका कोई व्यावहारिक फ़ायदा नहीं है, अत: उसकी प्राप्ति में समय नष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ज्ञान प्राप्ति का हक़दार है वह है जो वास्तविकता के मूल (यानी core of reality) से सम्बन्ध रखता हो। यही ज्ञान फ़र्ज़े-ऐन है। जो ज्ञान उसके बादवाले दायरे से सम्बन्ध रखता हो वह फ़र्ज़े-किफ़ाया होगा। ज्ञान और शिष्टता का जो दर्जा उसके भी बादवाले दायरे से सम्बन्ध रखता होगा वह ‘मिलहुल-इल्म’ कहलाएगा।
जो ज्ञान फ़र्ज़े-ऐन की हैसियत रखता है उसको तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह है जिसके लिए अरबी में एक शब्दावली प्रयोग की जा सकती है ما تصح بہ العقیدہ जिसका अर्थ है, “जिस ज्ञान के द्वारा इंसान का अक़ीदा (धार्मिक अवधारणा) ठीक हो जाए” यानी इस्लाम के अक़ीदों का वह कम-से-कम ज्ञान जिसके नतीजे में इंसान का अक़ीदा और रवैया दुरुस्त हो जाए। यानी आधुनिक पश्चिमी शब्दावली में जर्मन भाषा में इस्लाम का weltanschauung उसके सामने आ जाए। यह आवश्यक ज्ञान का सबसे पहला दर्जा है कि इंसान यह जान ले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं इस दुनिया में किस काम के लिए आया हूँ? इन सवालों के जवाब इंसान के पास होने चाहिएँ। अगर इंसान किसी ज़िम्मेदारी पर यहाँ भेजा गया है तो ज़िम्मेदारी के निर्धारण के लिए इन मौलिक सवालों का जवाब अनिवार्य है।
स्पष्ट रहे कि पवित्र क़ुरआन के अनुसार इंसान को एक ज़िम्मेदारी के साथ इस धरती पर भेजा गया है। पवित्र क़ुरआन में जहाँ आदम को धरती पर उतारने का ज़िक्र है वहाँ ‘हुबूत’ की शब्दावली प्रयुक्त हुई है। ‘हुबूत’ के शब्द को कुछ लोगों ने fall के शब्द से व्याख्यायित किया है, जो सही नहीं है। पवित्र क़ुरआन में हज़रत नूह के अवतरण के सिलसिले में भी कहा गया है “हमारी तरफ़ से सलामती और बरकतों के साथ कश्ती से उतरो।” (क़ुरआन, 11:48) गोया ‘हुबूत’ हो रहा है और पूरी इज़्ज़त के साथ हो रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ‘हुबूत’ के अर्थ में सज़ा की कोई परिकल्पना नहीं है।
उतरने के शब्द का अनुवाद कुछ पश्चिमी लेखकों ने fall के नाम से किया है। उन्होंने बाइबल और तौरात की धारणाओं की रौशनी में इसको देखा और यह समझा मानो सज़ा के तौर पर अल्लाह तआला ने आदम को जन्नत से निकाला था। पवित्र क़ुरआन में कहीं भी सज़ा का ज़िक्र नहीं है। पवित्र क़ुरआन में आदम (इंसान) की रचना से पहले ही यह कहा गया था कि ज़मीन में एक ख़लीफ़ा (सत्ताधारी) बनाना अभीष्ट है। “मैं धरती में (मनुष्य को) ख़लीफ़ा (सत्ताधारी) बनानेवाला हूँ।” (क़ुरआन, 2:30) अतः धरती में ख़िलाफ़त जन्म से पहले से निर्धारित थी। इसके बाद कहा गया कि ‘एबितू’ (उतरो)।
डॉक्टर हमीदुल्लाह ने एक जगह लिखा है कि जब इंसान कहीं पहुँचता है जो उसको भी उतरना कहते हैं। उदाहरणार्थ कहा जाता है कि हम कराची जाकर उतरे, लन्दन जाकर उतरे, मक्का मुकर्रमा जाकर उतरे। कई जगह पवित्र क़ुरआन में ‘हुबूत’ का शब्द किसी ज़िम्मेदारी को अंजाम देने की ग़रज़ से चार्ज लेने के सन्दर्भ में भी प्रयुक्त हुआ है। यहूदियों ने जब दुआ की कि अल्लाह तआला पवित्र धरती की हुकूमत हमें प्रदान कर तो उसके जवाब में अल्लाह तआला ने उनकी दुआ क़ुबूल की और यहूदियों को निर्देश दिया कि “इस शहर में चले जाओ जो माँगोगे मिलेगा।” (क़ुरआन, 2:61) यहाँ भी ‘हुबूत’ का शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ भी यही है कि ‘हुबूत’ का शब्द किसी सज़ा के तौर पर किसी बुलन्दी से नीचे की ओर फेंके जाने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकार के सम्मानित आगमन के साथ ज़िम्मेदारी संभालने के लिए पहुँच जाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए पवित्र क़ुरआन में ऐसी कोई धारणा मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में इंसान का अस्तित्व ख़ुद एक अपराध और एक सज़ा की क़िस्म रखता हो। ये तथ्य हर इंसान को मालूम होने चाहिएँ और ये उसके अक़ीदे का अनिवार्य हिस्सा हैं।
दूसरा दर्जा है ज्ञान का इतना हिस्सा जिसकी मदद से इबादत दुरुस्त तरीक़े पर अदा हो सके। हर इंसान कुछ-न-कुछ इबादतों को अदा करने की क्षमता रखता है। नमाज़ हर एक पर फ़र्ज़ है। रोज़ा स्वस्थ, वयस्क मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है साहिबे-निसाब पर वग़ैरा। अत: शरीअत के आदेशों का इतना ज्ञान कि इंसान की इबादतें दुरुस्त तरीक़े से अंजाम पा जाएँ यह फ़र्ज़े-ऐन है। इसके बाद इंसान जो ज़िन्दगी गुज़ारता है उस ज़िन्दगी गुज़ारने का शरीअत के अनुसार जो कम-से-कम ढंग है वह उसको आ जाए। ज़िन्दगी गुज़ारने का ढंग विभिन्न मैदानों में विभिन्न है। व्यापारी का ढंग और है, किसान का ढंग और है, शिक्षक का ढंग और है। जो व्यक्ति जिस मैदान में काम करता है उसको न केवल उस मैदान से सम्बन्धित शरीअत के मौलिक आदेश मालूम होने चाहिएँ, बल्कि ख़ुद इस कला के आदेश भी उसको आने चाहिएँ। यह समझना कि मैं अगर मेडिकल डॉक्टर हूँ तो शरीअत के आदेशों का तो पाबन्द हूँ, लेकिन चिकित्सा कला के नियमों का पाबन्द नहीं हूँ, यह ठीक नहीं है। यह समझना ग़लत है कि मेडिकल पेशे के प्रचलित आदेशों और नियमों की पाबन्दी शरीअत का आदेश नहीं है। शरीअत यह भी आदेश देती है कि अगर मैं चिकित्सा विज्ञान को बतौर पेशा अपना लूँ तो मुझे इस मैदान के नियमों एवं सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिए और उस ज़माने की दृष्टि से होना चाहिए जिस ज़माने में मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक हदीस में है कि अगर किसी व्यक्ति ने चिकित्सा पद्धति सीखे बिना किसी का इलाज किया है, और उसको कोई नुक़सान हो गया तो यह व्यक्ति ज़िम्मेदार होगा। यह जुर्माना अदा करेगा। कुछ फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्वयंभू डॉक्टर के हाथों ग़लत इलाज के नतीजे में अपंग हो जाए या मर जाए तो उस स्वयंभू को ‘दीयत’ (अर्थदंड) अदा करनी पड़ेगी। इससे पता चला कि इस कला के कलात्मक आदेशों को जानना भी फ़र्ज़े-ऐन है और इस कला से सम्बन्धित शरीअत के आदेशों को जानना भी इस कला के मुद्दई पर फ़र्ज़े-ऐन है।
यह तो ज्ञान का वह कम-से-कम दायरा है जो हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। दूसरा दायरा फ़र्ज़े-किफ़ाया का है जिसके बारे में इस्लामी फ़ुक़हा ने बहुत विस्तार से लिखा है। इमाम इब्ने-तैमिया, इमाम ग़ज़ाली और कई दूसरे लोगों ने यह बात लिखी है कि इन तमाम ज्ञान-विज्ञान की जानकारी मुसलमानों के लिए फ़र्ज़े-किफ़ाया की हैसियत रखती है जो मुस्लिम समाज को दूसरों पर आश्रित होने से बचाने के लिए अनिवार्य हैं। चुनाँचे इन तमाम उद्योगों का ज्ञान और उन कलाओं का ज्ञान जिनकी मुसलमानों को ज़रूरत है फ़र्ज़े-किफ़ाया है। मुसलमान को अपने व्यापार में, अपनी प्रतिरक्षा में, अपनी आज़ादी और दृढ़ता को बरक़रार रखने में जिस-जिस कला और निपुणता की ज़रूरत हो, उसकी प्राप्ति फ़र्ज़े-किफ़ाया है। फिर इमाम ग़ज़ाली ने इसपर दुख व्यक्त किया है। बहुत-से लोगों ने इन उलूम (ज्ञान) से दिलचस्पी लेना कम कर दी है। (इमाम ग़ज़ाली का हवाला मैं बार-बार इसलिए दे रहा हूँ कि उनको किसी दुनियादार आदमी के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि एक बहुत सख़्त धार्मिक इंसान के रूप में उनका परिचय है, बल्कि ख़ुद बहुत-से विद्वानों ने यहाँ तक कि इस्लाम के ज़िम्मेदार प्रवक्ताओं और प्रमाणित व्याख्याताओं ने इमाम ग़ज़ाली के कुछ ख़यालात को तनिक अतिवादी और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रया का परिणाम ठहराया है।)
इमाम ग़ज़ाली (रह॰) का कहना यह है कि इस ग़फ़लत का नतीजा यह निकला है कि हर व्यक्ति ने समझा कि दूसरे लोग यह ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और मैं इसकी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँगा। चुनाँचे लोग फ़िक़्ह का ज्ञान प्राप्त करने पर तो ध्यान देते हैं, चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान नहीं देते। लोग शरीअत का ज्ञान तो बड़ी दिलचस्पी और शौक़ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का ज्ञान प्राप्त नहीं करते। इसलिए कि शरीअत और फ़िक़्ह का ज्ञान प्राप्त करने से बड़े-बड़े पद मिलते हैं। क़ाज़ी का ओहदा मिलता है, मुफ़्ती का ओहदा मिलता है। शायद उस ज़माने में लोग बहुत अधिक शरीअत के ज्ञान की ओर आते होंगे। आज हमारे यहाँ फैकल्टी ऑफ़ शरीआ में दाख़िले के लिए अगर सौ छात्र आते हैं तो मैनेजमेंट साइंसेज़ में दाख़िले के लिए पाँच हज़ार आवेदक आते हैं। इसलिए कि एमबीए करने से अच्छी नौकरी मिलती है। शरीअत और उसूले-दीन पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती। उस ज़माने में इसके विपरीत होता था कि इल्मे-दीन पढ़नेवाले को अच्छी नौकरियाँ मिलती थीं, क़ाज़ी, फ़तवे और फ़िक़्ह के प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में इमाम ग़ज़ाली के मदरसे निज़ामिया में छात्र आते थे। चिकित्सा पढ़ने के लिए नहीं आते थे। इसलिए कि चिकित्सा के आधार पर मंत्रालय भी नहीं मिलता था, क़ज़ा (क़ाज़ी यानी न्यायाधीश का पद) भी नहीं मिलता थी। मुफ़्ती का ओहदा भी नहीं मिलता था।
बहरहाल इससे यह पता चला कि वे तमाम विशिष्टताएँ प्राप्त करना फ़र्ज़े-किफ़ाया है जो मुस्लिम समाज की प्रतिरक्षा, अस्तित्व और स्थिरता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इन दो दर्जों के अन्तर्गत आनेवाले ज्ञान-विज्ञान के अलावा जितने भी उलूम हैं, वे ‘मिलहुल-उलूम’ या ज्ञानपरक बिन्दु की हैसियत रखते हैं। अगर समाज में कुछ लोग इन उलूम को प्राप्त कर लें तो अच्छी बात है, सभ्यता और संस्कृति का विकास इससे प्राप्त होता है। बहुत-से सोशल साइंसेज़ हैं, मानवता के मामलात हैं। अगर कुछ लोग समाज में ख़त्ताती (Calligraphy) का पेशा अपनाते हैं, कुछ लोग समाज में इस तरह के कुछ और पेशे अपना लें तो इससे सभ्यता और संस्कृति में विशालता पैदा होगी। सभ्यता एवं संस्कृति में और ज़्यादा विकास होगा। लेकिन अगर पूरी क़ौम ख़त्ताती (Calligraphy) या ललित कला और शेरो-शाइरी में लग जाए तो फिर शेष मामलात प्रभावित होंगे और मुस्लिम समाज ग़ैर-मुस्लिमों पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए इमाम ग़ज़ाली ने इसपर बहुत विस्तार से विचार व्यक्त किए, बल्कि दुख व्यक्त किया है कि मुसलमानों ने फ़र्ज़े-ऐन और फ़र्ज़े-किफ़ाया के इस विभाजन को नज़रअन्दाज़ कर दिया है।
जब ज्ञान की बात आती है तो प्रशिक्षण की बात भी अनिवार्य होती है। ज्ञान प्रशिक्षण के बिना बेकार है। प्रशिक्षण और ज्ञान दोनों का एक-दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। बिना प्रशिक्षण के अगर ज्ञान होगा तो वह अल्लामा इक़बाल के शब्दों में ‘देवे-बे-रसन’ होगा। उन्होंने एक जगह पर ऐसे ज्ञान को जो नैतिक प्रशिक्षण के बिना प्राप्त हो जाए ‘देवे-बे-रसन’ कहा है। ऐसा राक्षस और ऐसा जिन्न जिसके गले में रस्सी नहीं है और वह आज़ाद होकर छूट जाए। समाज के लिए जितना विनाशकारी वह होगा उतना ही वह ज्ञानवान भी होगा जिसके पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण न हो और नैतिक गुणों से वह विभूषित न हो।
इस प्रशिक्षण के लिए क्या चीज़ अनिवार्य है, इसको इमाम ग़ज़ाली ने दो शीर्षकों के अन्तर्गत बयान किया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला की पहचान है। उनके शब्दों में “जब इंसान अपने आपकी, यानी अपने बन्दा होने की, अपने लाचार और मुहताज होने का सही ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो अल्लाह तआला की पहचान ख़ुद-ब-ख़ुद प्राप्त हो जाएगी। अत: जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने अल्लाह तआला की मारिफ़त (पहचान) ख़ुद ही प्राप्त कर ली।”
अल्लाह तआला की मारिफ़त (पहचान) प्राप्त करने का क्या तरीक़ा है। इसके लिए इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने बहुत-से शीर्षक बयान किए हैं। जिनमें से एक-दो नमूने के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले यह वास्तविकता कि इंसान की रचना और जन्म पूरी सृष्टि की रचना की एक निशानी है। दूसरे शब्दों में इंसान micro सतह पर एक पूरी सृष्टि है और पूरी सृष्टि macro सतह पर एक इंसान है। यह बात इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने बहुत विस्तार और स्पष्टता के साथ लिखी है। इसके बाद उन्होंने वही बात कही जो मैंने पहले भी कई बताई है कि इंसान में विभिन्न शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ रख दी गई हैं। उनमें से एक प्रवृत्ति मलकूतियत (फ़रिश्तों जैसे गुण) की और दूसरी प्रवृत्ति पाशविकता की है। इन दोनों प्रवृत्तियों को जब इंसान अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा आपस में समरूप कर लेता है और उनको दीन और शरीअत की माँगों के अनुसार बना लेता है तो दोनों का नतीजा सकारात्मक और सृजनात्मक होता है।
जब इंसान अल्लाह की मारिफ़त (पहचान) प्राप्त कर लेता है और अल्लाह तआला की महानता और प्रताप का एहसास उसके दिल में पूरी तरह बैठ जाता है तो फिर शुक्र और इबादत की भावना ख़ुद-ब-ख़ुद उसके दिल से फूटना शुरू हो जाती है। इबादत की भावना एक बार पैदा हो जाए तो वह इंसान को घमंड और बड़ाई के एहसास से रोके रखती है। इंसानों को इंसानों का ग़ुलाम बनाने से सुरक्षित रखती है। एक बार यह भावना पैदा हो जाए तो दुआ और इबादत के द्वारा इस भावना में और विकास होता रहता है। यही वजह है कि हदीस में कहा गया है कि “दुआ इबादत का मग़्ज़ (मूल तत्त्व) है।” इसलिए कि माँगने से इंसान की कमज़ोरी का इज़हार होता है। माँगना ख़ुद अपने ज़रूरतमन्द और तुच्छ होने की अभिव्यक्ति है। हीनता और विनम्रता की अभिव्यक्ति ही दरअस्ल इबादत की रूह और मूलात्मा है।
तमाम आसमानी शरीअतों ने किसी-न-किसी अन्दाज़ में इबादात की शिक्षा दी है। जिस तरह इस्लामी शरीअत एक परिपूर्णता की शान रखती है, उसी तरह इस्लाम की इबादतें भी परिपूर्णता की शान रखती हैं। तमाम पिछली शरीअतों में इबादात के जो-जो उचित तरीक़े प्रचलित थे उन सबको इस्लामी इबादतों में समो दिया गया। केवल नमाज़ की मिसाल अगर ले ली जाए तो व्यापकता और परिपूर्णता का यह गुण नुमायाँ तौर पर सामने आता है। शारीरिक इबादत के जितने रूप दुनिया में प्रचलित रहे हैं, वे तकवीनी (प्राकृतिक) दृष्टि से हों या तशरीअई (वैधानिक) दृष्टि से उन इबादतों का कोई-न-कोई महत्त्वपूर्ण और नुमायाँ अंग नमाज़ का अंग बना दिया गया है, ताकि नमाज़ उन सारी इबादतों का सार बन जाए। जिस तरह पवित्र क़ुरआन उन तमाम किताबों का सार बन गया है जो पिछले समयों में अवतरित की गईं।
इबादत और दुआ के लिए इंसान की शारीरिक पवित्रता भी ज़रूरी है और आध्यात्मिक पवित्रता भी। आध्यात्मिक पवित्रता के लिए नीयत का विशुद्ध और साफ़ होना और शारीरिक पवित्रता के लिए शरीर का पाक-साफ़ होना अनिवार्य है। व्यापकता और परिपूर्णता की यही शान पाँचों नमाज़ों के समयों के निर्धारण में पाई जाती है। पवित्र क़ुरआन में प्रत्यक्ष रूप से तो नमाज़ों के पाँचों समयों का उल्लेख नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से इन पाँचों समयों का हवाला मौजूद है। इन समयों में इबादत और नमाज़ों की फ़र्ज़ियत में क्या तत्त्वदर्शिता है, यह भी बयान किया गया है।
इबादत की इस्लामी धारणा पर बात करते हुए इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है कि एक अस्ल इबादत है जो दरअसल इबादत की core है। जो इस्लाम की बड़ी-बड़ी इबादतों पर सम्मिलित है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी इबादत है, अगर अल्लाह के आदेशों के अनुसार व्यतीत की जाए। इस इबादत के चार पहलू हैं। ‘अरकाने-चहारगाना बन्दगी’ (बन्दगी के चार स्तम्भ) यह कीमियाए-सआदत के एक अध्याय का शीर्षक है।
पहला स्तम्भ इबादात हैं (ये चार-पाँच इबादतें जो बड़ी-बड़ी हैं)
दूसरा स्तम्भ मामलात हैं (इंसान के अगर सारे मामलात शरीअत के अनुसार हों तो वे सब-के-सब इबादत की हैसियत रखते हैं)
तीसरा स्तम्भ मुहलिकात (यानी नापसन्दीदा नैतिकता से बचाव)
चौथा स्तम्भ मुनज्जियात (यानी पसन्दीदा नैतिक आचरण की प्राप्ति)
जब इंसान इबादत की इस ज़िन्दगी को अपनाना शुरू करता है तो एक से दूसरी इबादत में, दूसरी से तीसरी इबादत में, तीसरी से चौथी इबादत के मरहले में वह ख़ुद-ब-ख़ुद पहुँचना शुरू हो जाता है। एक दृष्टि से शरीअत की शिक्षा और क़ानून की सारी किताबें इन्ही चार इबादतों या अरकान (स्तम्भों) की विभिन्न शक्लें हैं। इंसान के मामलात चाहे व्यक्तियों के दरमियान हों, गिरोहों के दरमियान हों, दो क़ौमों के दरमियान हों या दो राज्यों के दरमियान हों। यह सब मामलात ही की विभिन्न क़िस्में हैं। इन मामलात को अगर शरीअत के अनुसार अंजाम दिया जाए तो ये सब-के-सब इबादत क़रार पाते हैं। वे राजनयिक गतिविधियाँ जो मुस्लिम समाज की सुरक्षा के लिए की जा रही हों, वह राजनयिक गतिविधि जो इस्लाम के लिए लड़नेवालों के समर्थन के लिए की जा रही हो, वह राजनयिक गतिविधि जो पीड़ित मुसलमानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए हो इबादत का दर्जा ले लेती है। इस प्रकार की तमाम इबादतें इमाम ग़ज़ाली (रह॰) की शब्दावली में रुक्ने-दोम (दूसरे स्तम्भ) में आती हैं। इसलिए कि इसके नतीजे में मुस्लिम समाज को सुरक्षा प्राप्त होती है और उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो क़ुरआन मजीद में जगह-जगह बताए गए हैं।
सआदत और नैतिकता इन दोनों के मध्य गहरा सम्बन्ध पवित्र क़ुरआन और हदीसों से स्पष्ट होता है, यही वजह है कि मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने, नैतिकता पर लिखनेवालों ने और बड़े सूफ़ियों ने ‘सआदत’ की शब्दावली बहुत अधिक प्रयोग की है। यह बात याद रखने के योग्य है कि ‘सआदत’ की इस शब्दावली का यूनानी शब्दावली happiness से कोई सम्बन्ध नहीं है, ख़ुशी और प्रसन्नता का यूनानी अर्थ और है और पवित्र क़ुरआन के अनुसार ‘सआदत’ का अर्थ और है। इस्लामी दार्शनिक या इस्लामी चिन्तक जब ‘सआदत’ का शब्द प्रयोग करते हैं तो कुछ कम समझ लोगों को ग़लत-फ़हमी हो जाती है कि शायद वे यूनानी शब्दावली happiness का अनुवाद ‘सआदत’ कर रहे हैं हालाँकि ये दोनों अलग-अलग शब्दावलियाँ हैं। एक प्रसिद्ध हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने नैतिकता और ‘सआदत’ से सम्बन्ध को यों स्पष्ट किया है कि من سعادۃ المرء حسن الخلق (शिष्टाचार में व्यक्ति की ‘सआदत’ है) यह हदीस इमाम बैहक़ी ने बयान की है कि इंसान की ‘सआदत’ का एक पहलू यह भी है, सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि उसका व्यवहार अच्छा हो। गोया सदाचार ‘सआदत’ की अनिवार्य अपेक्षा है और सदाचार का अनिवार्य नतीजा ‘सआदत’ है।
पवित्र क़ुरआन ने जहाँ जगह-जगह ‘सआदत’ और ‘सईद’ का ज़िक्र किया है, जहाँ जगह-जगह ‘शक़ी’ (अभागा, क्रूर) और ‘शक़ावत’ (दुर्भाग्य, क्रूरता) का उल्लेख किया है वहाँ पवित्र क़ुरआन ने महासिने-अख़्लाक़ (नैतिकता की ख़ूबियाँ) भी बयान किए हैं और नैतिक ख़राबियाँ भी याद दिलाई हैं। नैतिक पराकाष्ठा की सूची पवित्र क़ुरआन में बहुत लम्बी है, विभिन्न आयतों में मक्की और मदनी दोनों में ‘एहसान’ का उल्लेख बहुत अधिक मिलता है। ‘ज़विल-क़ुरबा’ यानी रिश्तेदारों के अधिकारों को अदा करना, उनपर ख़र्च करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका उल्लेख है। पवित्र क़ुरआन में सब्र और शुक्र का उपदेश जगह-जगह है, माफ़ी और ग़ुस्से को पी जाने का आदेश है। इसी तरह से बुराइयों से बचने का ‘फ़ुहशा’ (अश्लीलता और निर्लज्जता) और ‘मुनकर’ (बुरे कामों) से रोकने का ‘बग़्य’ और ‘बदगुमानी’ से बचने का, ‘ग़ीबत’ से बाज़ रहने का जगह-जगह आदेश दिया गया है। पवित्र क़ुरआन में ये नैतिक शिक्षाएँ न केवल अलग-अलग बयान की गई हैं, विभिन्न आयतों में इनका उल्लेख हुआ है, बल्कि इन तमाम नैतिक सिद्धान्तों और शिक्षाओं को क़ानूनी आदेशों से जोड़ दिया गया है।
ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लामी शिक्षा में क़ानून और नैतिकता दो परस्पर विरोधी चीज़ें नहीं हैं, या दो ऐसी समानान्तर रेखाएँ नहीं हैं जो साथ-साथ आगे बढ़ती हों और उनका आपस में कोई सम्बन्ध न हो, बल्कि ये दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं, क़ानून का आधार नैतिकता पर है और नैतिकता की माँगों पर कार्यान्वयन के लिए इस्लामी क़ानून का पालन ज़रूरी है। यह सम्भव नहीं है कि कोई व्यक्ति इस्लाम के आदेशों पर, शरीअत के व्यावहारिक आदेशों का पालन न करता हो और इस्लाम के निकट नैतिकता का आदर्श मान लिया जाए, यह भी सम्भव नहीं है कि कोई व्यक्ति नैतिकता के उच्च स्तर पर क़ायम हो, इस मापदंड पर जिसको शरीअत स्वीकार करती है और वह शरीअत के व्यावहारिक आदेशों पर कार्यरत न हो। यह दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर एक पर अमल किया जाएगा तो दूसरे पर कार्यान्वयन का सामान ख़ुद-ब-ख़ुद पैदा होगा।
ये शिष्टाचार जिनका विवरण हदीसों और पवित्र क़ुरआन की विभिन्न आयतों में बयान हुआ है उनपर जब इस्लाम के बड़े विद्वानों ने ज्ञानपरक ढंग से ग़ौर किया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰), हुज्जतुल-इस्लाम इमाम ग़ज़ाली (रह॰) और उनसे पहले बहुत-से लोगों ने तो इन तमाम धारणाओं को एक विशुद्ध बौद्धिक एवं वैचारिक ढंग से बयान करने का प्रायस किया। इसी तरह कोशिश की जिस तरह फ़ुक़हा ने फ़िक़ही आदेशों को संकलित किया, जिस तरह मुतकल्लिमीन ने इस्लामी अक़ीदों को संकलित किया, जिस तरह उलमाए-उसूल ने उसूले-फ़िक़्ह के आदेश संकलित किए, मुफ़स्सिरीन (टीकाकारों) ने तफ़सीर (टीका) के आदेश संकलित किए, उसी तरह उलमाए-अख़्लाक़ (नैतिकता के विशेषज्ञों) ने नैतिक आदेशों पर विवरण संकलित किए। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) का कहना यह है कि ये सारी नैतिकता दर अस्ल चार आधारों की विभिन्न शाखाएँ हैं। अगर यह कहा जाए कि नैतिकता एक बड़ा छाँवदार और फलदार वृक्ष है जिसके चार बड़े-बड़े तने हैं और उन चारों तनों से सारी शाखाएँ निकली हैं तो ऐसा कहना इमाम ग़ज़ाली की धारणा के बिलकुल अनुरूप होगा। इमाम ग़ज़ाली के विचार में चार बड़ी-बड़ी नैतिकताएँ हैं, जिनमें सबसे पहली नैतिकता हिकमत (तत्त्वदर्शिता), दूसरी शुजाअत (वीरता), तीसरी इफ़्फ़त (अपनी अस्मिता की रक्षा) और चौथी ‘अद्ल’ या अदालत है। तत्त्वदर्शिता से मुराद वह क्षमता है जिसके द्वारा इंसान अपने सारे उन कामों में जो वह अपने अधिकार से करता है, ग़लत और सही का निर्धारण कर सके। इंसान यह फ़ैसला कर सके कि क्या चीज़ नैतिक दृष्टि से दुरुस्त है और क्या नैतिक दृष्टि से दुरुस्त नहीं है। यह उसी समय हो सकता है जब उसको शरीअत के आदेशों का ज्ञान हो, शरीअत की नैतिक पराकाष्ठा की गहरी जानकारी हो, इस गहरी जानकारी और कार्यान्वयन के नतीजे में एक ऐसा ज़ेहन बन पाता है जो शेष तमाम मामलों में ख़ुद-ब-ख़ुद फ़ैसला करता रहता है कि कौन-सा क़दम सही है और कौन-सा ग़लत है। इंसान को ज़िन्दगी में हर समय, रात-दिन ऐसी समस्याएँ पेश आती हैं जिसमें उसको यह तय करना होता है कि क्या चीज़ नैतिक दृष्टि से सही है और क्या नैतिक दृष्टि से अप्रिय है।
अगर इंसान को शरीअत के मामलों में अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो, अगर वह शरीअत की नैतिकता को समझ चुका हो तो उसके लिए यह फ़ैसला बहुत आसान हो जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या ग़लत है। इसी क्षमता को इमाम ग़ज़ाली (रह॰) और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने हिकमत (तत्त्वदर्शिता) के शब्द से याद किया है। पवित्र क़ुरआन में भी ‘हिकमत’ का उल्लेख बार-बार आया है, “वह उन्हें किताब और हिकमत की शिक्षा देता है।” (क़ुरआन, 2:129) पवित्र क़ुरआन में जिस ‘हिकमत’ का ज़िक्र है वह बहुत आम है, इसमें सुन्नत भी शामिल है, इसमें वह समझ और अन्तर्दृष्टि भी शामिल है जो अल्लाह तआला किसी इंसान को प्रदान करता है। इस ‘हिकमत’ में शरीअत के बारे में वह गहरी समझ भी शामिल है जो शरीअत का अध्ययन करने के नतीजे में प्राप्त होती है।
‘अद्ल’ से मुराद वह स्वाभाविक सन्तुलन है जिसके द्वारा इंसान अपने ग़ुस्से और इच्छाओं को कंट्रोल में रख सकता है। अल्लाह तआला ने इंसान के अन्दर ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ (क्रोध-शक्ति) भी रखी है, अप्रिय बातों को देखकर उसके दिल में कड़ी प्रतिक्रिया पैदा होती है, उसके अन्दर इच्छाएँ हैं जो अगर हद में न रहें तो परेशानियों में मुब्तला करती हैं। इन इच्छाओं को ग़ुस्से के तक़ाज़ों को, और इंसान के मन की इच्छाओं को सन्तुलित कैसे रखा जाए, इसके लिए एक गुण दरकार है जिसे स्वाभाविक सन्तुलन कहते हैं जो शरीअत पर कार्यान्वयन के नतीजे में प्राप्त होता है, इस गुण को ‘अद्ल’ कहा गया है। तीसरी चीज़ ‘शुजाअत’ है, जिसको इमाम ग़ज़ाली नैतिकता के मूलस्रोतों में तीसरा मौलिक गुण क़रार देते हैं, ‘शुजाअत’ से मुराद इंसान की वह बौद्धिक क्षमता है जिसके द्वारा वह अपनी ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ को बुद्धि और शरीअत के अधीन रखता है। अगर उसका ग़ज़ब (ग़ुस्सा) बुद्धि और शरीअत के अधीन न हो तो वह ख़ुद भी तबाह होगा और दूसरों को भी बर्बाद करेगा। ‘शुजाअत’ से मुराद जैसा कि कुछ हदीसों से भी इसका समर्थन होता है, यह है कि इंसान अपने आपे में रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति के मौक़े पर अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को बुद्धि और शरीअत के अधीन रखे।
चौथा गुण ‘इफ़्फ़त’ है जो इंसान की इच्छाओं और वासनाओं को कंट्रोल में रखता है और उसको शरीअत और बुद्धि के अनुसार ढालता है। अगर ये चारों मौलिक नैतिकताएँ न हों, अगर नैतिक और इंसान की स्वाभाविक और मानसिक शक्तियों को कंट्रोल में रखनेवाली ये चारों लगामें न हों तो फिर नैतिक पराकाष्ठा का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता।
इमाम ग़ज़ाली ने ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ और ‘क़ुव्वते-शहवानिया’ (वासना-शक्ति), इन दोनों को बयान करने के लिए शिकारी कुत्ते की मिसाल दी है। अगर कुत्ते को सधा लिया जाए तो वह बहुत-से लाभकारी काम करता है, उसके द्वारा शिकार किया जा सकता है, जो जायज़ है, उससे जायज़ रोज़ी प्राप्त होती है, लेकिन अगर उसको न सधाया जाए तो वह परेशान करता है, काम बिगाड़ता है। इंसान को उसकी वजह से तकलीफ़ होती है। इसी तरह से ये चारों मौलिक नैतिकताएँ इंसान को कंट्रोल करती हैं और उसकी तमाम अनुभूतियों और भावनाओं को सीमाओं में रखती हैं।
जिस तरह उत्तम शिष्टाचार असीमित हैं उसी तरह नैतिक ख़राबियाँ भी अनगिनत हैं और उनके बहुत-से दर्जे हैं। उत्तम शिष्टाचार इसलिए असीमित हैं कि वे दरअस्ल अल्लाह तआला के शिष्टाचार का प्रतिबिंब हैं “अल्लाह के रंग में रंग जाओ, इसलिए कि अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है।” (क़ुरआन, 2:138) अत: जिस तरह उत्तम शिष्टाचार असीमित हैं इसलिए कि अल्लाह के शिष्टाचार असीमित हैं, उसी तरह नैतिक बुराइयों के भी अनगिनत दर्जे हैं, और हदीसों में इन सबसे बचने की दुआ बताई गई है। اللہم جنبنی منکرات الاخلاق (अल्लाहुम-म जन्निबनी मुनकरातिल-अख़्लाक़) अर्थात् “ऐ अल्लाह मुझे नैतिक बुराइयों से बचा!” यह इमाम तिरमिज़ी की रिवायत है। एक हदीस बयान हुई है जिसमें यह दुआ और यह जुमला प्रयुक्त हुआ है।
इन नैतिक ख़राबियों से बचना और नैतिक पराकाष्ठा से विभूषित होना ही व्यक्ति के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इन उत्तम शिष्टाचारों की सूची बहुत लम्बी है, ख़ुद इमाम ग़ज़ाली ने लगभग तीस शीर्षकों के तहत इन सब चीज़ों को बयान किया है तो बतौर मिसाल के बयान किया है। यह बयान करने के बाद वे यह कहते हैं कि शिष्टाचार का मौलिक सिद्धान्त यह है कि इंसान कमाले-हिकमत (तत्त्वदर्शिता की पराकाष्ठा) और कमाले-एतिदाल (अत्यन्त संयम) से काम ले, कमाले-हिकमत और कमाले-एतिदाल नैतिक पराकाष्ठा की कुंजी है। ‘क़ुव्वते-ग़ज़बिया’ के प्रयोग में अगर ग़ज़ब हक़ के लिए है तो वह एतिदाल और तत्त्वदर्शिता के अनुसार है। अगर ग़ज़ब अपने-आपके लिए है तो एक हद तक जायज़ है, इसके बाद अप्रिय और नाजायज़ की सामाएँ शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से ‘क़ुव्वते-शहवानिया’ है, अगर जायज़ सीमाओं के अन्दर प्रयोग हो, इस उद्देश्य के लिए प्रयोग हो कि अल्लाह तआला ने यह शरीर प्रदान किया है, इस शरीर की सुरक्षा, इसका स्थायित्व शरीअत पर कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो रोज़ा कैसे रखूँगा। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो अल्लाह के आदेशों का पालन कैसे करूँगा। अगर इस नीयत से अपने शरीर की, अपनी शारीरिक माँगों की सुरक्षा करता है तो यह शरीअत के पूरी तरह अनुरूप है।
यह एतिदाल दो तरीक़ों से प्राप्त हो सकता है। अल्लाह तआला के कुछ ख़ास बन्दे तो ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तआला स्वाभाविक रूप से यह नैतिकता प्रदान कर देता है, वे जन्म से ही बड़े अच्छे होते हैं, देखनेवाला महसूस करता है कि यह बच्चा बचपन ही से नैतिकता और चरित्र के उच्च स्थान पर आसीन है, ऐसे लोगों की पूरी जवानी सुथरी और पाक-साफ़ गुज़रती है। ये लोग बेदाग़ ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में मौजूद नकारात्मक शक्तियों से असर लेते हैं, समाज में मौजूद भौतिक प्रवृत्तियों से जल्द प्रभावित हो जाते हैं। समाज में मौजूद बुराई की शक्तियों को देखकर उनसे सबक़ सीखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वह नैतिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, संघर्ष करें। हर अच्छी चीज़ को सीखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है।
नैतिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि पहले नैतिक बुराइयों को निकाला जाए। नैतिक बुराइयों को समाप्त किया जाए। उसे ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय शरीअत ने बताए हैं, कुछ उपाय इस्लाम के बड़े विद्वानों ने, प्रशिक्षण और नैतिकता के विशेषज्ञों ने प्रस्तावित किए हैं, जो प्रस्ताव नैतिकता विशेषज्ञों ने प्रस्तावित किए हैं उनकी हैसियत एक इज्तिहादी राय की है। हर दौर के नैतिकता विशेषज्ञ और प्रशिक्षण विशेषज्ञ इससे मतभेद भी कर सकते हैं, तर्कों के साथ पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, संशोधन और बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। जो आदेश या उपाय शरीअत ने बताए हैं, उनपर हर दौर में कार्यान्वयन किया जाएगा। हलाल-हराम की सीमाएँ दरअस्ल नैतिक पराकाष्ठा का रास्ता आसान बनाने और नैतिक बुराइयों का रास्ता रोकने के लिए हैं। शरीअत ने जहाँ-जहाँ हलाल-हराम की सीमाएँ बयान की हैं, वह इसी ग़रज़ के लिए हैं कि नैतिक बुराइयों के रास्तों को बन्द किया जाए और नैतिक पराकाष्ठा के रास्तों को खोला जाए, शरीअत ने शिक्षा एवं प्रशिक्षण का आदेश दिया, शरीअत ने इबादतों का आदेश दिया, शरीअत ने बहुत-से ‘मुस्तहबात’ की शिक्षा दी, इन सबका उद्देश्य नैतिक पराकाष्ठा की प्राप्ति है। कुछ लोग यह समझते हैं और यह ख़याल कुछ अतिवादी विचार रखनेवाले लोगों के लेखों या व्यवहार या उनके बारे में प्रसिद्ध कहानियों और बे-बुनियाद क़िस्सों से पैदा हुआ है कि शरीअत का अभीष्ट यह है कि इंसान के अन्दर जो पाशविक प्रवृत्तियाँ या इच्छाएँ हैं, उदाहरणार्थ भूख है, प्यास है, दूसरी आवश्यकताएँ हैं, उनको बिलकुल समाप्त कर दिया जाए और सिरे से मिटा दिया जाए, ऐसा दुरुस्त नहीं। ऐसा करना सुन्नते-रसूल के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के स्वभाव और शरीअत की रूह से टकराता है। इन गुणों को ख़त्म करना अभीष्ट नहीं है, जिस काम या कोशिश को सूफ़ियों की शब्दावली में ‘मुजाहदा’ कहा गया है उससे मुराद वह ऐच्छिक प्रयास है जिसके नतीजे में इन शिष्टाचारों को, इन प्रवृत्तियों को सीमाओं के अन्दर रखा जाए और बुद्धि और शरीअत के अनुसार बनाया जाए। नैतिक पराकाष्ठा कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, उत्तम शिष्टाचार जहाँ भी पाए जाएँ वे प्रशंसनीय हैं। इस्लामी शरीअत ने उनको पसन्द किया है, उनको स्वीकार किया है। हातिमताई की बेटी का क़िस्सा प्रसिद्ध है, एक जंग में जो उस क़बीले के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी जिससे हातिमताई की बेटी का सम्बन्ध था, हातिमताई की बेटी की जहाँ रिश्तेदारी थी, उसके ख़िलाफ़ जंग हुई, दुश्मनों को शिकस्त हुई और मैदाने-जंग में जो लोग मौजूद थे वे क़ैद करके मदीना मुनव्वरा लाए गए। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अगले दूसरे दिन जंगी क़ैदियों में जो महिलाएँ या बच्चे थे उनकी हालत मालूम करने के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक महिला बड़ी गौरवशाली मालूम होती थी और लगता था कि यह महिला किसी बहुत उच्च परिवार से सम्बन्ध रखती है। उसने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सम्बोधित करके कहा कि “मैं अपने क़बीले के सरदार की बेटी हूँ, अपनी क़ौम के सरदार की बेटी हूँ, मेरे पिता लोगों का समर्थन किया करते थे, कमज़ोरों की सहायता किया करते थे, क़ैदियों को छुड़ाया करते थे, भूखों को खाना खिलाया करते थे, अम्न और शान्ति क़ायम रखने में प्रयासरत रहते थे, उन्होंने कभी किसी सवाली का सवाल नहीं टाला, मैं हातिमताई की बेटी हूँ।” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “ऐ लड़की! यह तो वाक़ई मुसलमानों के और ईमानवालों के शिष्टाचार हैं।” फिर उन्होंने फ़रमाया, “इस लड़की को छोड़ दो! इस लड़की का बाप नैतिक पराकाष्ठा को पसन्द करता था और अल्लाह भी नैतिक पराकाष्ठा को पसन्द करता है।” इसपर एक सहाबी ने पूछा कि “ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वाक़ई अल्लाह तआला नैतिक पराकाष्ठा को पसन्द करता है?” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “क़सम है उस सत्ता की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जन्नत में वही दाख़िल होगा जिसका आचरण अच्छा होगा। इससे पता चला कि नैतिक पराकाष्ठा जहाँ भी हो वह प्रशंसनीय है और उसको शरीअत पसन्द करती है। नैतिक पराकाष्ठा के बारे में शरीअत ने दो मापदंड बयान किए हैं, एक मापदंड तो वैचारिक और ज्ञानपरक मापदंड है जो क़ुरआन और सुन्नत के लिखित संग्रह में मौजूद है, जिसकी इस्लामी विद्वानों ने ज्ञानपरक व्याख्या की, जिसका संक्षिप्त-सा सार मैंने बयान किया। नैतिक पराकाष्ठा का दूसरा मापदंड व्यावहारिक है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रवैये से ज़ाहिर होता है, नैतिकता के जितने मूल स्रोत हैं, जितने नैतिक सौन्दर्य हैं वे सब-के-सब अपनी पराकाष्ठा के साथ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में मौजूद हैं। जो व्यक्ति नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदर्श के जितना क़रीब है वह नैतिक दृष्टि से उतना ऊँचा है, जितना दूर है उतना नीचा है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आचरण पवित्र क़ुरआन का चलता-फिरता नमूना था। यह प्रसिद्ध हदीस तो हम सबने सुनी है जिसमें हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने फ़रमाया कि “अल्लाह के रसूल के आचरण वही थे जो पवित्र क़ुरआन में लिखे हुए हैं।” गोया नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक चलता-फिरता क़ुरआन थे। यही वजह है कि इस्लाम के बड़े विद्वानों ने हमेशा कोशिश की कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी और आचरण को इस तरह आम किया जाए, इस तरह जनसाधारण के सामने बयान किया जाए कि इस्लामी नैतिकता और रवैये का एक चलता-फिरता नमूना हमारे सामने आ जाए। वह चलता-फिरता नमूना जब हमारे सामने आ जाए तो इंसान के लिए नैतिक पराकाष्ठा का पालन करना आसान हो जाता है।
इंसानों की अधिकांश संख्या की कमज़ोरी यह है कि वे किसी विचारधारा से कम प्रभावित होते हैं, किसी ख़याल और सोच से कम प्रभावित होते हैं, वास्तविकता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप उच्च-से-उच्च विचारधारा, उच्च-से-उच्च शिक्षा और उच्च-से-उच्च सोच को केवल वैचारिक ढंग में बयान करें तो बहुत कम लोग उससे सहमत होंगे, लेकिन उसी वास्तविकता को चलता-फिरता दिखा दें, जो काम करना चाहते हैं वह करके सामने रख दें तो अधिकांश संख्या में लोग उससे प्रभावित होते हैं और बड़ी संख्या में लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने जहाँ-जहाँ नैतिक पराकाष्ठा की सैद्धान्तिक शिक्षा दी है, वहाँ विभिन्न पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) की ज़िन्दगियों के नमूने भी सामने रखे हैं। ये छब्बीस (26) व्यक्तित्व जिनका उल्लेख पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह किया गया है, यह छब्बीस नैतिक पराकाष्ठा के बड़े-बड़े नमूने हैं जो चलते-फिरते नज़र आते हैं और उन सबके गुण हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में इकट्ठा हो गए हैं। जिनकी नैतिक पराकाष्ठा ख़ुद पवित्र क़ुरआन में भी जगह जगह बयान हुई है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी के विभिन्न पहलू पवित्र क़ुरआन में हमेशा-हमेशा के लिए रिकार्ड कर दिए गए हैं।
यों ये दोनों मिलकर इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो पवित्र क़ुरआन प्राप्त करना चाहता है यानी नैतिक पराकाष्ठा की पूर्ति। जब नैतिक पराकाष्ठा की पूर्ति हो जाती है तो ‘बिर्र’ और ‘एहसान’ और ‘सआदत’ का वह उद्देश्य प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति के लिए इंसानियत भटकती रही है। यूनान के दार्शनिकों से लेकर भारत के ऋषियों तक, और रोमी क़ानूनविदों से लेकर आधुनिक काल के विशेषज्ञों तक, इंसान जिस चीज़ की प्राप्ति में भटकता रहा है वह यही है कि इंसान को अस्ली और वास्तविक सफलता कैसे प्राप्त हो। जिस चीज़ को वह ख़ूबी समझता है वह क्या है और कैसे प्राप्त हो सकती है, जिस चीज़ को वह सफलता क़रार देता है वह क्या है और उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है। यही वह सवाल है जिसका जवाब पूरी शरीअत और शरीअत की सारी शिक्षा है।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने एक जगह लिखा है कि ‘बिर्र’ यानी नेकी की व्यापक क़िस्म जो तमाम ख़ूबियों को, तमाम उत्तम आचरणों को, सआदतों के तमाम आयामों को अपने अन्दर समेटे हुए है, उसका आधार तीन सिद्धान्तों पर है, तौहीद (एकेश्वरवाद), तसदीक़ (पुष्टि), रिसालत (पैग़म्बरी) और अल्लाह की शरीअत के सामने सिर झुका देना। अगर ये तीनों चीज़ें पूरी हो जाएँ तो इंसान नैतिक पराकाष्ठा के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है और मानवता की उस तड़प को दूर कर सकता है जो हर दौर में और हर इलाक़े में संवेदनशील इंसानों को परेशान करती रही है। ‘बिर्र’ क़ी वास्तविकता बयान करते हुए शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि ‘बिर्र’ में वे सभी कर्म शामिल हैं जो इंसान इसलिए करता है कि वह अल्लाह के आदेशों के अनुसार और अल्लाह के बयान किए हुए कर्म से स्वयं को समरूप कर ले, अत: हर वह कर्म जो दुनिया और आख़िरत या उनमें से किसी एक के लिए किसी बेहतरी का ज़रिया बनता है वह कर्म ‘बिर्र’ यानी नेकी में शामिल है। नेकी से मुराद केवल विशुद्ध धार्मिक कर्म नहीं हैं, बल्कि ‘बिर्र’ से मुराद या नेकी से मुराद हर वह अच्छा काम है जिसका अच्छा नतीजा दुनिया या आख़िरत में निकले। चूँकि आख़िरत स्थायी और आदिकालिक और शाश्वत है इसलिए आख़िरत का नतीजा भी शाश्वत और आदिकालिक है, इसलिए आख़िरत का नतीजा अवश्य ही दुनियवी परिणामों से श्रेष्ठ है। इसी तरह से हर वह कर्म जिससे इंसानों के मामलात में बेहतरी पैदा हो, इंसानों की ज़िन्दगी में बेहतरी आए, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में quality of life बेहतर हो, वह कर्म भी शाह साहब की राय में ‘बिर्र’ और नेकी का काम है। इसलिए कि यह भावना अल्लाह ने इंसान के अन्दर रखी है कि वह अपने मामलों को बेहतर-से-बेहतर बनाना चाहता है, अपनी जीवन-प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक और सुन्दर बनाना चाहता है। जायज़ तरीक़े से, नैतिक सीमाओं के अन्दर यह उद्देश्य प्राप्त किया जाए तो यह एक नेक उद्देश्य है और इसको नेकी शुमार किया जाएगा। इसी तरह से हर वह अमल जो इंसान को अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए तैयार करे और उसकी बुद्धि और अन्तर्दृष्टि पर अगर कोई पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा दे या कम कर दे वह भी नेकी में शामिल है।
सच तो यह है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ‘बिर्र’ के शीर्षक से जो कुछ बयान किया है वह पूरब और पश्चिम के अधिकांश चिन्तकों की धारणाओं का वह सारांश है जिसको उन्होंने इस्लाम और शरीअत के समरूप करके बयान किया है। यूनानियों ने जो लिखा, भारत के चिन्तकों ने जो सोचा, आज के पश्चिमी चिन्तक जो सोचते हैं या चाहते हैं और इस्लामी विद्वानों ने जो कुछ सोचा और समझा इस सबके उल्लेख निकालकर उन्होंने इस तरह एक व्यापक धारणा में समो दिया है कि इससे शरीअत की व्यापकता और परिपूर्णता पूरे तौर पर सामने आती है। इसी तरह से गुनाह या ‘इस्म’ से मुराद हर वह कर्म है जो इन सबके विलोम हो, हर वह कर्म जो इंसान को शैतानी इच्छाओं के क़रीब ले जाए, जो इंसानों के लिए बुरा हो, जो उनके आपसी सम्बन्धों को ख़राब करने का कारण बने, यानी इंसानों की इस कोशिश को नाकाम बनाए कि उनकी ज़िन्दगी के मामले बेहतर और ज़्यादा मुकम्मल हों, या इंसान की बुद्धि और अन्तर्दृष्टि पर इससे पर्दा पड़ जाए, ऐसा हर काम शरीअत की नज़र में गुनाह है और अप्रिय है।
व्यक्ति जब नैतिकता की प्राप्ति की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम उसको ज़ब्ते-नफ़्स (मन को नियंत्रित रखने) का करना पड़ता है। ज़ाहिर है इच्छाओं से बचने का काम ज़ब्ते-नफ़्स के बिना नहीं हो सकता। अल्लामा इक़बाल ने भी जहाँ ‘ख़ुदी’ की पूर्णता के मरहले और दर्जे बताए हैं वहाँ ज़ब्ते-नफ़्स को बहुत महत्त्व से बयान किया है। ज़ब्ते-नफ़्स के बिना प्रशिक्षण नहीं हो सकता, ज़ब्ते-नफ़्स के बिना ‘ख़ुदी’ का निर्माण और पूर्णता की प्रक्रिया सम्भव नहीं है। ज़ब्ते-नफ़्स का एक दर्जा तो वह है जो शरीअत के मुहर्रमात (शरीअत द्वारा हराम ठहारए हुए कामों और रिश्तों) से बचने के नतीजे में पैदा हो जाता है। शरीअत की ‘मकरूहात’ (नापसन्द ठहराई हुई चीज़ों और कामों) से बचने की कोशिश की जाए तो ज़ब्ते-नफ़्स ख़ुद-ब-ख़ुद पैदा हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी समाज में बदी की शक्तियाँ इतनी प्रबल और प्रभावी होती हैं कि इन शक्तियों से बचने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर किसी मनोरंजन स्थल में जाना, बाज़ार में जाना, किसी पार्क में टहलना या झूलना अच्छा काम है। इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर इंसान स्वास्थ्य और व्यायाम की नीयत से किसी मनोरंजन स्थल में जाए तो यह काम शरीअत में पसन्दीदा है, लेकिन अगर किसी जगह ऐसे स्थान हों जहाँ बदअख़्लाक़ी हो रही हो, जहाँ बदअख़्लाक़ी का जुर्म करनेवाले कसरत से जमा होते हों, वहाँ जाने से इंसान को एहतिराज़ करना चाहिए। ज़ब्ते-नफ़्स के ख़िलाफ़ है, प्रशिक्षण के काम पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए अगर कोई प्रशिक्षण विशेषज्ञ वहाँ जाने से रोक दे तो यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि शरीअत ने तो पार्क में जाने से नहीं रोका, पवित्र क़ुरआन में तो बाग़ में जाने से मना नहीं किया गया, हदीस में तो मना नहीं किया गया, फिर अमुक बुज़ुर्ग ने क्यों मना किया है। इस तरह की आपत्ति मात्र फ़ालतू है और प्रशिक्षण की माँगों को न समझने की वजह से है। अस्ल उद्देश्य यह है कि “सफल हो गया वह जिसने उसे (अपने मन को) विकसित किया और असफल हुआ वह जिसने उसे दबा दिया।” (क़ुरआन, 91:9-10) मन की शक्तियों को पवित्र बनाना और उनको ख़राब होने और ज़्यादा ख़राब होने से रोकना, यह पहला क़दम है जो ज़ब्ते-नफ़्स के लिए अनिवार्य है।
ज़ब्ते-नफ़्स के लिए जहाँ शरीअत ने मुहर्रमात (हराम ठहराए हुए रिश्तों और चीज़ों) से बचने का आदेश दिया है वहाँ इबादत करने की शिक्षा भी दी है। इबादत एक तो वह अस्ल और वास्तविक इबादत है जो इंसान दिन में पाँच समय करता है, रमज़ान में रोज़े रखता है, ज़कात के रूप में करता है, हज करता है, तिलावते-क़ुरआन (क़ुरआन पाठ) करता है, इबादत करता है। लेकिन एक और अर्थ के अनुसार पूरी ज़िन्दगी इबादत हो सकती है। अगर शरीअत के अनुसार गुज़ारी जाए, शरीअत के उद्देश्यों को सामने रखकर गुज़ारी जाए।
यहाँ इबादत से मुराद इबादत का वह सीमित या ख़ास अर्थ है जिसकी वास्तविकता है, “अल्लाह के आदेशों के आगे अत्यन्त विनम्रता का प्रदर्शन।” यह इस्लामी विद्वानों ने इबादत की परिभाषा की है। अल्लाह के सामने विनम्रता का यह प्रदर्शन शरीर के साथ भी हो, मुख से भी हो, दिल से भी हो और भावनाओं और अनुभूतियों के साथ भी हो। जब यह प्रदर्शन अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के अनुसार किया जाता है तो यह इंसानों को इंसानों का ग़ुलाम बनने से सुरक्षित रखता है। घमंड और ग़ुरूर से इंसानों को रोकता है। जब इंसान अल्लाह से माँगता है तो माँगना भी तुच्छता और विनम्रता का प्रदर्शन है, यही कारण है कि कहा गया कि “दुआ इबादत की रूह और मग़्ज़ है।” और यह रूह इस तरह है कि अल्लाह से माँगा जाए और अल्लाह के सिवा किसी और से न माँगा जाए।
इबादत के लिए शरीअत ने पाकीज़गी और पवित्रता का आदेश भी दिया है, पवित्रता ख़ुद एक इबादत है। सम्भवतः इस्लाम के सिवा किसी और धर्म में पाकीज़गी को, सफ़ाई और सुथराई को इस तरह इबादत का हिस्सा नहीं बनाया गया जिस तरह इस्लाम में बनाया गया है। आन्तरिक पवित्रता के दावेदार तो बहुत-से धर्म हैं, लेकिन शारीरिक पवित्रता की वह कल्पना कम पाई जाती है जिसकी पवित्र क़ुरआन ने और हदीसों ने शिक्षा दी है। जब इंसान शारीरिक रूप से सफ़ाई-सुथराई अपनाता है तो इसका प्रभाव आन्तरिक पवित्रता पर भी पड़ता है। ज़ाहिरी पाकीज़गी एक संकेत है अन्दर की गंदगी को साफ़ करने के लिए। इंसान बहुत-से काम ऐसे करता है जो स्वाभाविक रूप से अप्रिय होते हैं, जो इंसानों को उनकी पाशविक पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं, इस गंदगी को साफ़ करने के लिए, इस मरहले से निकलकर दोबारा मलकूतियत (फ़रिश्तोंवाले गुणों) के मरहले में दाख़िल होने के लिए शारीरिक पवित्रता अनिवार्य है। इस पवित्रता से एक नए मरहले में दाख़िल होने का एहसास होता है। जब इंसान इबादत की ख़ातिर वुज़ू करता है और इबादत की नीयत से मुसल्ले (नमाज़ पढ़ने की दरी या चटाई) पर खड़ा होता है तो गोया एक नए चरण में प्रवेश कर रहा होता है और इस नए चरण में प्रविष्ट होने का आभास जागरूक और ताज़ा करने के लिए शारीरिक पवित्रता का आदेश दिया गया है।
इंसानों का स्वभाव यह है कि जब इंसान किसी नए मरहले में दाख़िल हो रहा होता है तो शरीर को भी पवित्र और ताज़ा करता है और लिबास भी पाक-साफ़ पहनता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको नहलाने के बाद नया लिबास पहनाया जाता है। जब कोई समारोह होता है तो इंसान नहा-धोकर नया लिबास पहनता है। शादी होती है तो ग़ुस्ल (स्नान) करके नया लिबास पहनता है। जब किसी नौजवान को नौकरी मिलती है तो अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी पर जाने से पहले वह नौजवान ग़ुस्ल करता है और नया लिबास पहनकर नौकरी पर जाता है। इन मिसालों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस्म और लिबास की पवित्रता से इंसान में एक नए पन का क़ौमी एहसास पैदा होता है और इस नए पन के एहसास तले वह नई ज़िन्दगी का आरम्भ करता है।
अल्लाह के सामने हर हाज़िरी एक नई ज़िन्दगी है। आध्यात्मिकता और ऊपरी लोक से सम्बन्ध के मामले में हर हाज़िरी से एक नई ज़िन्दगी मिलती है, एक नई लीज़ आफ़ लाइफ़ प्राप्त होती है। अत: तहारत और पाकीज़गी के ज़ाहिरी और शारीरिक महत्त्व के साथ-साथ आन्तरिक और मनोवैज्ञानिक महत्त्व को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। शरीअत ने कुछ ख़ास हालात में ग़ुस्ल का या तो आदेश दिया है या नसीहत की है। आम हालात में वुज़ू काफ़ी है। वुज़ू में केवल उन अंगों का धोना काफ़ी क़रार दिया गया है, जिनसे इंसान आम तौर पर भौतिक गन्दगियों, पाशविक गतिविधियों और शैतानी प्रेरकों को पूरा करने में काम लेता है। यों उन अंगों को धोकर साफ़ कर लेने से उन गन्दगियों के प्रभाव भी साफ़ हो जाते हैं जिनमें उन अंगों को संलिप्त किया गया था। शारीरिक और आध्यात्मिक पवित्रता के बाद अल्लाह से निकटता और उसके सामने हाज़िरी का मरहला आता है। अनुभव गवाह है कि जितने मनोयोग, तैयारी और निष्ठा भाव से नमाज़ की तैयारी की जाती है उतना ही अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास बढ़ता है। बन्दे का फ़र्ज़ तो यह था कि दिन-रात में कम-से-कम पचास बार हाज़िरी का सौभाग्य प्राप्त करता लेकिन शरीअत प्रदान करनेवाले पालनहार ने बन्दों की कमज़ोरी और भूल जाने की आदत के सामने पाँच ही को पचास के बराबर क़रार दे दिया। यों भी उसके यहाँ एक निष्ठापूर्ण नेकी पर दस गुना अज्र (प्रतिदान) का वादा किया गया है। इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने ‘कीमियाए-सआदत’ में इबादत या बन्दगी के चार महत्त्वपूर्ण और बड़े-बड़े रुक्न (स्तम्भ) गिनवाए हैं। उनको उन्होंने ‘अरकाने-चहारगाना बन्दगी’ के शीर्षक से बयान किया है।
- पहला रुक्न : इबादत
- दूसरा रुक्न : मामलात
- तीसरा रुक्न : मुहलिकात, यानी नैतिकता को नष्ट कर देनेवाले, जिनसे बचना ज़रूरी है।
- चौथा रुक्न : मुनज्जियात, यानी वे पसन्दीदा शिष्टाचार जिनकी प्राप्ति दुनिया और आख़िरत में मुक्ति और सफलता पाने के लिए अनिवार्य है।
पहले रुकन यानी इबादतों के बड़े-बड़े विभाग दस हैं। (1) अक़ीदे का सही होना (2) ज्ञान प्राप्त करना। (3) तहारत और पाकीज़गी (4) नमाज़ (5) रोज़े (6) ज़कात (7) हज (8) क़ुरआन पढ़ना (9) अल्लाह का ज़िक्र (10) औराद और वज़ाइफ़।
दूसरे रुक्न, यानी मामलात के भी दस बड़े-बड़े विभाग हैं। यानी (1) खाने-पीने के शिष्टाचार (2) निकाह और घरेलू मामलों के शिष्टाचार (3) व्यापार और लेन-देन के शिष्टाचार (4) हलाल रोज़ी प्राप्त करना (5) इंसानों से सम्पर्क और सम्बन्ध के शिष्टाचार (6) तन्हाई के शिष्टाचार (7) सफ़र यानी यात्रा के शिष्टाचार (8) आदाबे-सिमाअ (सुनने के शिष्टाचार) (9) अम्र बिल-मारुफ़ और नही अनिल-मुनकर (भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना) (10) राज्य और समाज के मामलात।
इसी तरह तीसरे रुक्न के, यानी मुहलिक और अप्रिय नैतिकता जिनसे बचना ज़रूरी है, दस उप विभाग हैं। (1) सबसे पहले बुरी आदतों या यानी नफ़्से-अम्मारा का इलाज (2) शहवात (वासनाओं) और शारीरिक माँगों का सुधार और कंट्रोल (3) ज़बान के द्वारा फैलनेवाली ख़राबियाँ (4) कपट और ईर्ष्या की बुराइयाँ (5) दुनिया की हद से ज़्यादा मुहब्बत (6) माल की हवस (7) नाम और शोहरत की इच्छा, दिखावा (9) घमंड और बड़ाई का एहसास (10) ख़ुद-फ़रेबी, ग़फ़लत और गुमराही।
चौथे रुक्न, यानी मुनज्जियात के भी इमाम ग़ज़ाली ने दस बड़े-बड़े विभाग गिनाए हैं। ये वे
उत्तम शिष्टाचार हैं जिनसे इंसान को विभूषित होना चाहिए। ये विभाग निम्नलिखित हैं—
(1) तौबा यानी अल्लाह के सामने दोबारा लौट आने का ऐच्छिक और फ़ाइनल फ़ैसला और उसका पालन (2) सब्र और शुक्र (3) ख़ौफ़ और रिजा (अल्लाह से डरना और उसकी दयालुता की उम्मीद भी रखना) (4) फ़क़्र (सन्तोष) और ज़ुह्द (संयम) (5) सच्चाई और निष्ठा (6) मुहासबा (अपना हिसाब ख़ुद करना) और मुराक़बा (ध्यान) (7) चिन्तन-मनन (8) तौहीद (एकेश्वरवाद) और तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा (9) शौक़ और मुहब्बत (10) मौत और आख़िरत की ज़िन्दगी को याद रखना।
यह वह ख़ाका (रूपरेखा) है जो इमाम ग़ज़ाली ने अपनी इतिहास रचनेवाली पुस्तक ‘एहयाउल-उलूमिद्दीन’ में, ‘कीमियाए-सआदत’ और ‘अल-मुर्शिदुल-अमीन’ में विस्तार से बयान किया है। इन चालीस शीर्षकों में कुछ अति महत्त्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा इन लेक्चर्स में सामने आ गई है। यहाँ इस ख़ाके को सामने रखने का उद्देश्य यह याद दिलाना है कि यह शरीअत मात्र कुछ क़ानून के संग्रह का नाम नहीं है, बल्कि यह ज़िन्दगी की एक भरपूर व्यवस्था और सभ्यता-तथा संस्कृति का एक निराला पैराडायम है। दरअसल यही याद-दहानी लेक्चर्स के इस सिलसिले का मूल उद्देश्य और उत्प्रेरक है।
Recent posts
-

इस्लामी शरीअत का भविष्य और मुस्लिम समाज का सभ्यता मूलक लक्ष्य (शरीअत : लेक्चर# 12)
02 December 2025 -
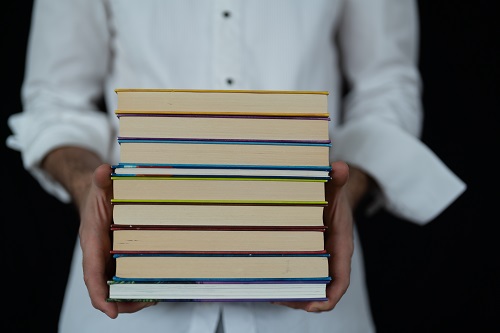
इस्लामी शरीअत आधुनिक काल में (शरीअत : लेक्चर# 11)
25 November 2025 -

इल्मे-कलाम अक़ीदे और ईमानियात की ज्ञानपरक व्याख्या एक परिचय (शरीअत : लेक्चर# 10)
21 November 2025 -

अक़ीदा और ईमानियात - शरई व्यवस्था का पहला आधार (शरीअत : लेक्चर# 9)
17 November 2025 -

तज़किया और एहसान (शरीअत : लेक्चर# 8)
12 November 2025 -

तदबीरे-मुदन - राज्य और शासन के सम्बन्ध में शरीअत के निर्देश (शरीअत : लेक्चर# 7)
05 November 2025