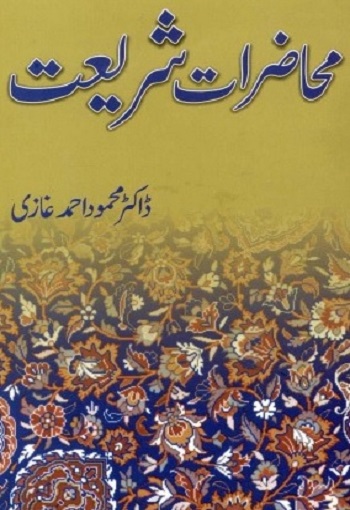
मुसलमान और मुस्लिम समाज (शरीअत : लेक्चर # 3)
-
शरीअत
- at 28 August 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
(इस्लाम की बुनियाद में मुस्लिम समाज एक केंद्रीय अवधारणा है, जो न केवल एक समुदाय का निर्माण करती है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आदर्श बिरादरी का प्रतीक है। डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी द्वारा दिए गए शरीअत लेक्चर #3 में, "मुसलमान और मुस्लिम समाज" विषय पर गहन चर्चा की गई है। पवित्र कुरआन के अनुसार, इस्लाम का सबसे बड़ा सामूहिक लक्ष्य मुस्लिम समाज का गठन है, जिसकी जड़ें हज़रत इबराहीम (अ.स.) की दुआ और बैतुल्लाह (काबा) के निर्माण से जुड़ी हैं। अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने अपनी शरीअत के साथ-साथ इस विश्वव्यापी समाज की स्थापना की, जो तौहीद, सार्वभौमिकता, हिजरत और समता पर आधारित है। लेक्चर में 'उम्मत' और 'मिल्लत' के अंतर, इमाम की भूमिका, एकता की निशानियाँ, न्याय का सिद्धांत, और मुस्लिम समाज के कर्तव्य जैसे भलाई का आदेश देना व बुराई से रोकना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुवादक गुलज़ार सहराई द्वारा हिंदी में प्रस्तुत यह लेक्चर मुस्लिम समाज की विशिष्टताओं को उजागर करता है, जो आज के वैश्विक संदर्भ में भी प्रासंगिक है। यदि आप इस्लामिक समाज, शरीअत और आध्यात्मिक एकता को समझना चाहते हैं, तो यह लेक्चर आवश्यक है। आगे पढ़ें और इस्लाम की गहराई में उतरें! --संपादक)
आज की चर्चा का शीर्षक है “मुसलमान और मुस्लिम समाज”। मुस्लिम समाज को आसान भाषा में मुस्लिम समाज या मुस्लिम बिरादरी भी कहा जा सकता है। पवित्र क़ुरआन के अनुसार इस्लाम का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम सामूहिक लक्ष्य मुस्लिम समाज का गठन है। पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह मुसलमानों को मुस्लिम समाज से जुड़े रहने का, मुस्लिम समाज के उद्देश्यों और लक्ष्य को पूरा करने का उपदेश और निर्देश दिया गया है। पवित्र क़ुरआन से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम समाज के स्थायित्व की दुआ और भविष्यवाणी हज़ारों वर्ष पहले हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ने की थी। यह उस समय की बात है जब वह मुस्लिम समाज के लिए एक महसूस और आभासी आध्यात्मिक केन्द्र यानी बैतुल्लाह (काबा) का निर्माण कर रहे थे।
यह मुस्लिम समाज जिसका आभासी केन्द्र हज़ारों वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुका था, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का सबसे बड़ा उपकार और सबसे बड़ी देन है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) दो चीज़ें इंसानियत को देकर इस दुनिया से गए। एक अपनी शरीअत जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के रूप में हमारे सामने आई है और दूसरे वह मुस्लिम समाज जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ायम किया, जिसके गठन और निर्माण में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी ज़िन्दगी का अधिकांश भाग लगाया। इस मुस्लिम समाज की सुरक्षा इस्लाम का सबसे बड़ा लक्ष्य है, इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के शब्दों में कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय की स्थापना अस्ल उद्देश्य है, यानी ख़ुद अपने-आपमें अभीष्ट है, इसको किसी और उद्देश्य की ज़रूरत नहीं है। एक फ़क़ीह ने लिखा है कि शरीअत के वाजिबात की दो क़िस्में हैं। एक उद्देश्यों की अनिवार्यता और दूसरी संसाधनों की अनिवार्यता। उद्देश्यों की अनिवार्यता से अभिप्रेत वे अनिवार्यताएँ हैं जो ख़ुद अपने-आपमें अनिवार्य हैं। संसाधनों की अनिवार्यता में वे अनिवार्यताएँ शामिल हैं जो किसी और अनिवार्य कार्य के माध्यम के रूप में अपनाई गई हों, जिनके द्वारा और किसी बड़े वाजिब या बड़े फ़र्ज़ को पूरा करना अभीष्ट हो।
मुस्लिम समुदाय की इस स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने इस मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व में आने की दुआ की थी और कहा था कि “ऐ परवरदिगार! हम दोनों बाप-बेटों को अपना सच्चा आज्ञाकारी मुसलमान बना और हमारी औलाद में एक ऐसा मुस्लिम समुदाय पैदा कर जो तेरा आज्ञाकारी हो और तेरे दीन का ध्वजावाहक हो।” (क़ुरआन, 2:128) यह मुस्लिम समाज चूँकि विश्वव्यापी मुस्लिम समाज बना था, इसलिए हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के हाथों इसका बीज डलवाया गया। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) इस दृष्टि से दूसरे पैग़म्बरों में बहुत नुमायाँ हैं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम की ओर लोगों को बुलाने का आरम्भ किया। विभिन्न महाद्वीपों में गए और अरब द्वीप के अलावा अफ़्रीक़ा महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर और कुछ इतिहासकारों के बयान के अनुसार यूरोप महाद्वीप और कुछ और इतिहासकारों के बयान के अनुसार एशिया महाद्वीप के इलाक़े भारत में भी हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) का आगमन हुआ और इन सब इलाक़ों में तौहीद (एकेश्वरवाद) के सन्देश को फैलाया। इस दृष्टि से हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) से मुस्लिम समाज का जुड़ाव एक विशेष सार्थकता रखता है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के अनुयायियों के आदर्श रवैये और सांस्कृतिक और सभ्यता सम्बन्धी निशानियाँ जिनको ‘मिल्लत’ के नाम से याद किया गया है, इस मिल्लत को हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की मिल्लत क़रार दिया गया है और बताया गया कि “तुम्हारे बाप इबराहीम का पन्थ जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था” (क़ुरआन, 22:78) कि यह रवैया जो तुमने अपनाया है, यह सभ्यता का प्रतीक तुम्हारे मुस्लिम समाज का यह तरीक़ा, यह इबादात जो तुम अंजाम दे रहे हो, यह दीन जिसपर तुम चल रहे हो, इन सबका मूल और आधार इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की शिक्षा में है, इसका केन्द्र वह बैतुल्लाह है जिसका निर्माण इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने किया और यह उस क़ुर्बानी की भावना की यादगार है जो इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने बैतुल्लाह के आसपास में पेश की थी।
इस दृष्टि से मुस्लिम समाज को मिल्लते-इबराहीमी क़रार दिया जाना एक अत्यन्त अर्थपूर्ण बात है, मिल्लते-इबराहीमी के मौलिक गुणों में सार्वभौमिकता, हिजरत, और रंग-नस्ल के भेद से विरक्ति के गुण बहुत नुमायाँ हैं। पवित्र क़ुरआन में जहाँ-जहाँ हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के कथन उद्धृत हुए हैं उनमें यह बात बहुत नुमायाँ है कि मैं हर प्रकार के रंग-नस्ल पर आधारित भेदभावों से विरक्त होता हूँ, शिर्क के सभी रूपों से अलग होता हूँ, बल्कि बहुदेववादियों के ख़िलाफ़ जो मेरे दिल में ना-पसन्दीदगी है, शिर्क के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की भावना मेरे दिल में मौजूद है, उसको व्यक्त करता हूँ, यह बात पवित्र क़ुरआन में अनेक आयतों में बयान हुई है। तौहीद से यह गहरा जुड़ाव, रंग-नस्ल से यह दो टूक विरक्ति, शिर्क से यह स्पष्ट नफ़रत इस बात की माँग करती है कि हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के सन्देश में सार्वभौमिकता पाई जाए। तौहीद (एकेश्वरवाद) और सार्वभौमिकता एक-दूसरे के पूरक हैं। तौहीद स्रष्टा की तार्किक माँग है कि तौहीदे-मख़लूक़ पर भी ईमान रखा जाए। अगर सृष्टि का रचयिता एक है तो उसकी मख़लूक़ (जानदार) होने में सब बराबर हैं, सबको समान रूप से उसकी सृष्ट रचना और उसके इबादतगुज़ार होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए किसी एक बन्दे को दूसरे बन्दों पर किसी एक ग़ुलाम को दूसरे ग़ुलाम पर वरीयता जताने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तमाम इंसान बराबर हैं। अगर तमाम इंसान बराबर हैं तो फिर तमाम इंसानों पर आधारित एक विश्व बिरादरी क़ायम होनी चाहिए।
अगर सार्वभौमिकता के सिद्धान्त को मान लिया जाए तो फिर हिजरत के सिद्धान्त को मानना बहुत आसान है। अगर इंसान यह स्वीकार कर ले कि जिस इलाक़े में वह पैदा हुआ है उस इलाक़े को कोई श्रेष्ठता अल्लाह की ज़मीन के दूसरे हिस्सों पर प्राप्त नहीं है। जिस गिरोह या बिरादरी में मेरा जन्म हुआ है, उस गिरोह या बिरादरी के रंग, नस्ल, ज़बान और शेष भौगोलिक भेदभावों को कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है तो फिर उसके लिए अल्लाह के दीन की ख़ातिर, अल्लाह के सन्देश को आम करने की ख़ातिर एक इलाक़े से दूसरे इलाक़े में जाना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना और एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा बसना आसान हो जाता है, और यह कोई मुश्किल बात नहीं रहती।
इसलिए मिल्लते-इबराहीमी की ये तीन विशेषताएँ, यानी हिजरत, सार्वभौमिकता, तौहीद यानी रंग-नस्ल के भेद से विरक्ति और एक ईश्वर और सारे इंसानों के एक आदम से पैदा होने का अक़ीदा, ये तमाम विशेषताएँ मिल्लते-इबराहीमी में पाई जाती हैं। और यही विशेषताएँ मुस्लिम समाज की ख़ास विशेषताएँ हैं। ‘उम्मत’ और ‘मिल्लत’ कुछ पूर्वी ज़बानों में विशेष रूप से फ़ारसी और तुर्की में पर्यायवाची शब्द समझे जाते हैं। एक हद तक ये पर्यायवाची हैं भी, लेकिन इन दोनों के प्रयोग और चरितार्थ होने में बारीक-सा अन्तर है। ‘उम्मत’ जिसका स्पष्टीकरण अभी आगे होगा, इससे मुराद तो वह बिरादरी है जिससे मुसलमानों का सम्बन्ध है, लेकिन यह बिरादरी मात्र दूसरी अनगिनत बिरादरियों की तरह की कोई आम बिरादरी नहीं है, बल्कि उसका आधार एक सन्देश पर है, इसका उद्देश्य एक सांस्कृतिक सन्देश को लेकर चलना है, यह कुछ अल्लाह के प्रतीकों की ध्वजावाहक है, यह अल्लाह के दीन पर कार्यरत है, अल्लाह के एक होने का दर्शन इसका मौलिक सिद्धान्त है। इन तमाम विशिष्टताओं तथा भेदभावों का प्रदर्शन उसके रवैये और सभ्यता में होता है। इन सभ्यता-सम्बन्धी निशानियों और सांस्कृतिक नमूनों को जिनमें अल्लाह की निशानियाँ भी शामिल हैं, सामूहिक रूप से ‘मिल्लत’ के शब्द से याद किया जाता है।
‘मिल्लत’ के अर्थ में ‘दीन’ (धर्म) भी शामिल है, मिल्लत के अर्थ में मुस्लिम समुदाय की सामूहिकता भी शामिल है। मिल्लत के अर्थ में मुस्लिम समुदाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य भी शामिल हैं और मिल्लत के अर्थ में मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक उद्देश्य तथा प्रतीक भी शामिल हैं।
‘उम्मत’ का शब्द अरबी ज़बान के शब्द ‘उम्म’ से निकला है। सब जानते हैं कि ‘उम्म’ का मूल अर्थ अरबी भाषा में ‘माँ’ भी है और ‘वृक्ष की जड़’ के भी है। किसी इमारत की आधारशिला के लिए भी ‘उम्म’ का शब्द प्रयुक्त होता है और किसी चीज़ की अस्ल के लिए भी यह शब्द आता है। ये सब शब्द या अर्थ एक साझे अर्थ का प्रमाण बनते हैं, जिसमें आरम्भ के एकत्व, उद्देश्य के एकत्व और यात्रा के एकत्व की धारणाएँ शामिल हैं। जिस तरह एक माँ की सन्तान एकजुट और सर्वसहमत होती है, उसका आरम्भ भी एक होता है, उसकी ज़िन्दगी एक साथ गुज़रती है, जिनमें आपस में अत्यन्त गहरी मुहब्बत, सम्बन्ध और भाई-चारा पाया जाता है, जिनके उद्देश्य भी एक ही होते हैं, पारिवारिक लक्ष्य साझे होते हैं, इसी तरह से मुस्लिम समाज का आरम्भ भी एक है, लक्ष्य भी एक हैं, और रास्ता और मंज़िल भी एक ही है। यानी सत्यमार्ग, जिस तरह एक वास्तविक माँ यानी ‘उम्म’ की सन्तान, एक बिरादरी होती है उसी तरह मुसलमानों की आध्यात्मिक माओं, यानी उम्महातुल-मोमिनीन की सन्तान भी एक बिरादरी है, जिनका आरम्भ भी एक है, अंजाम भी एक और रास्ता यानी सत्यमार्ग भी एक ही है।
पवित्र क़ुरआन में जब यह बताया गया कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पाक पत्नियाँ मुसलमानों की माएँ हैं, तो यह दरअसल इसी सम्बन्ध की ओर इशारा था जो सम्बन्ध एक परिवार के लोगों में दोस्ती, भाई-चारे और प्रेम का होना चाहिए। एक माँ की औलाद के दरमियान, जिस तरह की हमदर्दी पाई जानी चाहिए, उसी तरह का सम्बन्ध, दोस्ती और हमदर्दी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की स्थापित की हुई ‘उम्मते-मुस्लिमा’ (मुस्लिम समुदाय) में होना चाहिए। इसी आयत का विवरण या और अधिक व्याख्या के तौर पर कुछ सहाबा ने अपनी क़ुरआन की प्रति में लिख दिया था ‘वहु-व अबू लहुम’ (और अल्लाह के रसूल उनके आध्यात्मिक बाप हैं) यह बात कुछ हदीसों में भी बयान हुई है जिसमें अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सम्बन्ध का प्रकार मुसलमानों से वही बताया गया है जो एक बाप का अपनी सन्तान से होता है। पवित्र क़ुरआन की शैली यह है कि वह बहुत संक्षेप से काम लेता है और संक्षेप के कारण कुछ ऐसे बयानों को स्पष्ट नहीं करता जो एक बुद्धिमान पाठक ख़ुद-ब-ख़ुद समझ लेता है। चुनाँचे पवित्र क़ुरआन में यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि ‘वहु-व अबू लहुम’ (और अल्लाह के रसूल सल्ल॰ उनके आध्यात्मिक बाप हैं) लेकिन जब एक बार यह कह दिया गया कि “उनकी पाक पत्नियाँ मुसलमानों की माएँ हैं” तो यह बात ख़ुद-ब-ख़ुद स्पष्ट हो गई कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुसलमानों के आध्यात्मिक बाप हैं।
यह ‘उम्मत’ जो शब्द ‘उम्म’ से निकला है, एक ऐसी जमाअत है जिसका आरम्भ, अंजाम, यात्रा का साधन, यात्रा का रास्ता, पाथेय, रास्ते की रौशनी, सब चीज़ें एक और साझी हैं, ये कुछ नैतिक विशेषताओं से विभूषित है और विभूषित होनी चाहिए। ‘उम्मते-मुस्लिमा’ का सम्बन्ध संख्या से नहीं होता। संख्या तो कमो-बेश भी हो सकती है, कभी-कभी अगर एक ही व्यक्ति ऐसा हो जो सही आधार पर क़ायम हो, मुस्लिम समाज के लक्ष्य के लिए सक्रिय हो, उस एक व्यक्ति को भी ‘उम्मत’ के नाम से याद किया गया है “इबराहीम अकेले एक उम्मत थे जो अल्लाह के सामने एकाग्रचित होकर खड़े हो गए।” (क़ुरआन, 16:120)
‘उम्मत’ का शाब्दिक अर्थ एक और भी है। और वह अर्थ यह है कि ‘उम्मत’ से मुराद वह गन्तव्य स्थान है जिस ओर लोग सफ़र करके आया करें। अरबी भाषा में ‘फ़ुअला’ का वज़न किसी लक्ष्य या अभीष्ट के लिए आता है जिसकी तरफ़ रुख़ करके वह कार्य अंजाम दिया जाए। अत: ‘उम्मत’ का अर्थ होगा ‘जिसकी ओर इरादा किया जाए, जिसकी ओर इरादा करके लोग आएँ और सफ़र करें।’ ज़ाहिर है जिसकी तरफ़ लोग इरादा करके आएँगे वह मंज़िले-मक़्सूद (गन्तव्य स्थान) ही होगा। गोया मुस्लिम समाज का अस्तित्व अस्ल मंज़िल की निशानदेही करता है। अगर इंसानियत को मंज़िले-मक़्सूद मालूम करनी है तो वह मुस्लिम समाज से जुड़ जाए, मुस्लिम समुदाय जिस रास्ते पर जा रहा है वह रास्ता ख़ुद-ब-ख़ुद अस्ल मंज़िल तक पहुँचा देगा। अगर कहीं कोई बहुत बड़ा क़ाफ़िला किसी सफ़र पर जा रहा हो और कुछ लोग रास्ता भटक जाएँ, जंगलों और रेगिस्तानों में गुम हो जाएँ तो उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही होता है कि यह देखें कि बड़ा क़ाफ़िला किस तरफ़ जा रहा है, वे बड़े क़ाफ़िले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मंज़िले-मक़्सूद का रास्ता मालूम करना और वहाँ तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े क़ाफ़िले का पता लगाना आसान होता है। गोया मुस्लिम समाज की हैसियत उस बड़े क़ाफ़िले की-सी है जिसकी तरफ़ इक्का-दुक्का मुसाफ़िर, रास्ते से भटक जानेवाले राही और दूसरे लोग जो रास्ते की तलाश में हों वे सम्पर्क करते हैं। ऐसे गुमराह लोगों के लिए रास्ते की तलाश का आसान रास्ता यह है कि मुस्लिम समाज से जुड़ जाएँ और उस रास्ते पर चल पड़ें जिसपर मुस्लिम समाज चल रहा है। ऐसा करेंगे तो गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाएँगे।
यह बात अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने भी कुछ शख़्सियतों के बारे में इरशाद फ़रमाई। चुनाँचे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के चचा जो इस्लाम से पहले तौहीद को मानते थे और इसकी वजह से अरब के बहुदेववादियों की सख़्तियों और अत्याचारों का शिकार हुए और उन अत्याचारों की वजह से घर-बार छोड़ने पर मजबूर हुए और आख़िरकार परदेस में रहते हुए इस दुनिया से विदा हो गए, उनके बारे में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा कि “ऐ अल्लाह के रसूल! जिस तरह की शिक्षा आप देते हैं इसी तरह की बातें मेरे चचा भी बताया करते थे, मेरे चचा के साथ क़ियामत में क्या सुलूक होगा?” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “एक उम्मत के तौर पर उठाया जाएगा।” इसी तरह की बात एक और व्यक्ति क़ुस्स-बिन-साइदा के बारे में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाई जो इस्लाम से पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, तौहीद (एकेश्वरवाद) और उच्च नैतिकता का ध्वजावाहक था, तथा अरब के बहुदेववादियों के अत्याचारों से परेशान रहता था।
‘उम्मत’ जब अस्तित्व में आएगी तो ज़ाहिर है किसी लक्ष्य के लिए काम करेगी, वह लक्ष्य सिराते-मुस्तक़ीम (सत्यमार्ग) पर सफ़र और पारलौकिक तथा सांसारिक सफलता की प्राप्ति है। लेकिन कोई सफ़र भी बिना क़ाफ़िले के सरदार के या अमीरे-कारवाँ के बिना पूरा नहीं हो सकता।
इस्लाम ने हर चीज़ में अनुशासन का आदेश दिया है। अतः जीवन के हर पहलू को अत्यन्त अनुशासन के साथ गुज़ारना चाहिए, यहाँ तक कि अगर दो आदमी भी सफ़र कर रहे हों तो निर्देश दिया गया है कि वे अपने में से एक को अमीर नियुक्त कर लें और उसके मार्गदर्शन, निगरानी और अनुशासन के अनुसार काम करें। अगर दो लोगों के बारे में यह आदेश है तो पूरे मुस्लिम समुदाय के बारे में यह आदेश क्यों नहीं होगा। अत: मुस्लिम समाज का इमाम भी होना चाहिए। एक दृष्टि से, बल्कि वास्तविक अर्थ में तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुस्लिम समाज के इमाम हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया से चले जाने के बाद व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शरीअत की रौशनी में मुस्लिम समुदाय को मंज़िले-मक़्सूद पर ले जाने के लिए मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, इस मार्गदर्शक के लिए इस्लामी साहित्य में ‘इमाम’ की शब्दावली प्रयुक्त हुई है।
‘इमाम’ का शब्द भी ‘उम्म’ से निकला है। जिस माद्दे (धातु) से ‘उम्मत’ का शब्द निकला है उसी माद्दे से ‘इमाम’ का शब्द भी निकला है। ‘इमाम’ और ‘उम्मत’ का गहरा सम्बन्ध है जैसा कि इस माद्दे और अस्ल से सम्बन्ध से ज़ाहिर है। ‘इमाम’ अरबी भाषा में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है और ये सारे अर्थ मुसलमानों के ‘इमाम’ यानी लीडर में मौजूद होने चाहिएँ। वह क़ाइद (लीडर) बहुत बड़ी जमाअत का क़ाइद हो, पूरी मुस्लिम उम्मत का क़ाइद हो, ख़लीफ़तुल-मुस्लिमीन हो या छोटे-छोटे गिरोहों का सरदार हो, किसी छोटे इलाक़े का क़बीले का, राज्य का, छोटे देश का शासक हो, इसमें ये सारे अर्थ बहरहाल मौजूद होने चाहिएँ। इमाम का एक आम अर्थ तो क़ाइद और पेशवा का है, वह तो सबको मालूम है, लेकिन इमाम का एक अर्थ ‘किताबे-हिदायत’ (मार्गदर्शक पुस्तक) भी है। एक ऐसी मार्गदर्शक पुस्तक का है जो रास्ता बताती हो, मंज़िले-मक़्सूद की निशानदेही करती हो, रास्ते की मुश्किलों को दूर करने में मार्गदर्शन करती हो और यह बताती रहती हो कि रास्ता चलने की माँगें क्या हैं, गन्तव्य स्थान कहाँ स्थित है। वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। चुनाँचे पवित्र क़ुरआन में आसमानी किताबों को ‘इमाम’ कहा गया है। “जिस तरह यह किताब यानी पवित्र क़ुरआन इमाम है इसी तरह इससे पहले हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) पर नाज़िल की जानेवाली किताब इमाम भी थी और रहमत भी थी।” (क़ुरआन, 46:12) गोया जिस तरह पवित्र क़ुरआन मार्गदर्शक पुस्तक है, अल्लाह का डर रखनेवालों को हाथ पकड़कर गन्तव्य स्थान तक पहुँचा देती है और तमाम इंसानों को रास्ता दिखाती और बताती है, आम लोगों के लिए भी मार्गदर्शन है और अल्लाह का डर रखनेवालों के लिए भी मार्गदर्शक है, इसी तरह मुसलमानों के लीडर को मार्गदर्शक और रहनुमा भी होना चाहिए। उसको चाहिए कि वह सत्यमार्ग को ख़ुद भी समझता और जानता हो और अपने अनुयायियों को सत्यमार्ग तक पहुँचाने में मदद भी दे सकता हो। सुविधाएँ भी उपलब्ध कर सकता हो। अगर किसी व्यक्ति में यह क्षमता नहीं है, न वह सत्यमार्ग को जानता है, न सत्यमार्ग तक जाना चाहता है, न अपने अनुयायियों को सत्यमार्ग पर चलाना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति ग़ैर-मुस्लिमों का नायक तो हो सकता है, मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता।
‘इमाम’ का दूसरे अर्थ एक ऐसा राजमार्ग भी है जिसपर चलना आसान हो और जिसपर चलकर गन्तव्य स्थान तक पहुँचा जा सके। पवित्र क़ुरआन में इमाम का शब्द एक स्पष्ट और खुले राजमार्ग के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। “और बेशक वे दोनों बस्तियाँ एक खुले रास्ते या कुशादा राजमार्ग पर स्थित थीं।” इससे पहले एक गुज़ारिश में बताया जा चुका है कि शरीअत का अर्थ वह खुला और स्पष्ट सीधा रास्ता है जो मुसलमानों को पारलौकिक सफलता के लक्ष्य तक पहुँचा दे। गोया एक दृष्टि से शरीअत और ‘इमाम’ दोनों का अर्थ एक है। अगर इमाम ख़ुद भी सीधे रास्ते पर है और दूसरों को भी साथ लेकर सीधे रास्ते चल रहा है, शरीअत का सीधा राजमार्ग पर लेकर जा रहा है तो वह सचमुच इमाम है और क़ाइद है। और अगर वह शरीअत के राजमार्ग पर नहीं चल रहा तो फिर वह मार्गदर्शक नहीं है कुछ और है। ये सारे अर्थ इमाम के शब्द में पाए जाते हैं और इन शाब्दिक अर्थों से अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि ‘इमाम’ और ‘उम्मत’ इन दोनों का आपस में अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है।
पवित्र क़ुरआन के विद्यार्थी जानते हैं कि पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह ऐसी शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं, संकेतात्मक और अलंकारिक रूप में, जिनका सम्बन्ध यात्रा और यात्रा के लिए अनिवार्य वस्तुओं से है। जब आदमी सफ़र पर निकलता है, पुराने ज़माने में जब क़ाफ़िलों में निकलता था, ऊँट या घोड़े की पीठ पर या पैदल तो अपने साथ पाथेय भी लेकर निकलता था, रास्ते में ज़ाहिर है न खाना मिलता था न पानी मिलता था। रेगिस्तानों, जंगलों और पर्वतीय रास्तों में सफ़र करना पड़ता था तो पाथेय का महत्त्व असाधारण था, बिना पाथेय के किसी व्यक्ति के लिए सफ़र करना सम्भव नहीं था, न छोटा सफ़र न बड़ा।
पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह पाथेय का ज़िक्र है। कहा गया है, “बेहतरीन पाथेय जो इस रास्ते पर सफ़र के लिए दरकार है वह तक़्वा (ईशपरायणता) का पाथेय है।” (क़ुरआन, 2:197) रास्ते में रौशनी की ज़रूरत भी पड़ती थी, इसलिए कि रात को भी सफ़र करना है, रेगिस्तान में भी करना है, पहाड़ों में भी करना है, नदी-नाले भी पार करने हैं। रात को रौशनी के बिना सफ़र नहीं हो सकता। अँधेरी रातें भी होती हैं, इसलिए पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह नूर का भी ज़िक्र है, बिना नूर के, बिना रौशनी के अन्धेरे में, रात में सफ़र करना सम्भव नहीं है। यही वजह है कि पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह वे तमाम शब्दावलियाँ प्रयोग की गई हैं जिनका सम्बन्ध सफ़र और यात्रा के संसाधनों से है। ख़ुद मुसलमान दिन में सत्रह बार जिस चीज़ की दुआ करता है वह सिराते-मुस्तक़ीम (सीधे रास्ते) पर चलने की और सत्यमार्ग स्पष्ट होने की दुआ करता है। सत्यमार्ग सफ़र के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। ‘अइम्मा’ और ‘इमाम’ के यही अर्थ हैं जिनकी वजह से इन दोनों में आपस में सम्पर्क क़ायम होता है।
मुस्लिम समाज के वास्तविक और सबसे बड़े इमाम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिए पवित्र क़ुरआन में ‘उम्मी’ का गुण जगह-जगह प्रयुक्त हुआ है। उसमें भी गहरी सार्थकता पाई जाती है। ‘उम्मी’ का शब्द भी ‘उम्म’ से निकला है। ‘उम्मी’ का एक अर्थ तो प्रसिद्ध है और उसको हर मुसलमान जानता है, ‘उम्मी’ का यह अर्थ वह है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नुबूवत के बड़े सुबूतों में से एक है। नबी के मोजिज़ात (चमत्कारों) में से एक बड़ा मोजिज़ा है। ‘उम्मी’ उसको कहते हैं जिसने किसी मकतब में या किसी उस्ताद के सामने विधिवत रूप से शिक्षा न पाई हो। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बहुत-से अरबों की तरह बचपन में या तो जवानी में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। लिखने-पढ़ने का कोई सामान अरब में और विशेष रूप से मक्का में मौजूद नहीं था। इसलिए मक्का के आम नौजवानों की तरह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी भी गुज़री, उसके बाद यकायक अल्लाह तआला ने इल्म और बसीरतों के सरचश्मे उनकी मुबारक ज़बान से जारी करवा दिए। जो इस बात का प्रमाण हैं कि इन सब ज्ञान एवं तत्त्वदर्शिताओं का मुख्य स्रोत अल्लाह की ओर से आनेवाली ‘वह्ये-इलाही’ है, कोई सांसारिक शिक्षा प्राप्ति नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहीं एक दिन भी किसी मकतब (मदरसे) में शिक्षा पाई होती तो नुबूवत के बाद बीसियों दावेदार खड़े हो जाते। हर एक यह दावा करता नज़र आता कि ये ज्ञान हमने सिखाए हैं, कोई कहता अमुक ने सिखाए थे, लेकिन हर व्यक्ति जानता था और आज भी जानता है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसा कोई एहसान किसी का नहीं उठाया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ज़िन्दगी में किसी के उपकार का बोझ नहीं उठाया, जिनका उपकार मिला उनके उपकार को पूरा-पूरा स्वीकार किया। अपने चचा के उपकारों को स्वीकार किया। अपने गुफा के साथी अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का उपकार याद किया। इन दो के अलावा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने किसी के उपकार का भार ज़िन्दगी में नहीं उठाया और अल्लाह ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को किसी का आभारी नहीं रखा, विशेष रूप से उन असाधारण ज्ञान-विज्ञान के मामले में जो केवल जिबरील अमीन के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुबारक ज़बान से जारी हुए।
लेकिन ‘उम्मी’ के इन ख़ास अर्थों के अलावा ‘उम्म’ से निकलनेवाली चीज़ को भी ‘उम्मी’ कहते हैं। यानी ‘उम्मी’ से मुराद वह है जो अस्ल पर क़ायम हो, अपनी ‘उम्म’ (जड़) पर क़ायम हो, ‘उम्मी’ से मुराद वह भी है जिसका सम्बन्ध ‘उम्मुल-क़ुरा’ से हो। ‘उम्मुल-क़ुरा’ मक्का मुकर्रमा का लक़ब (उपनाम) था, मक्का मुकर्रमा को तमाम बस्तियों की माँ यानी अस्ल और जड़ कहा जाता था। तमाम बस्तियों के लोग ‘उम्मुल-क़ुरा’ से सम्पर्क करके आया करते थे। ‘उम्मुल-क़ुरा’ की हैसियत केन्द्र की थी। एक ऐसे केन्द्र की थी जिसकी तरफ़ तमाम इलाक़ों से लोग आया करते थे, इसलिए उसको ‘उम्मुल-क़ुरा’ के शब्द से याद किया गया है। जिसका सम्बन्ध ‘उम्मुल-क़ुरा’ से हो उसको भी ‘उम्मी’ कहा गया। अरबों को ‘उम्मीयीन’ दो कारणों से कहा जाता था। एक तो ‘उम्मीयीन’ का सम्बन्ध ‘उम्मुल-क़ुरा’ से था या ‘उम्मुल-क़ुरा’ में आने-जानेवालों से था। ‘उम्मुल-क़ुरा’ से श्रद्धा रखनेवालों से था, इसके साथ-साथ ‘उम्मीयीन’ उनको इसलिए भी कहा गया कि उनमें अधिकांश संख्या पढ़ने-लिखने से बिलकुल अनजान और ज्ञान-विज्ञान और हर प्रकार की समझ और संस्कृति से अनजान थी। इसलिए उनको ‘उम्मी’ के शब्द से याद किया गया।
अरबी भाषा में ‘उम्मत’ का एक और अर्थ किसी जीवन व्यवस्था, दिशा निर्देश और तौर-तरीक़े का भी है। यानी वह जीवन-प्रणाली जिस पर समष्टीय रूप से लोग कार्यरत हों उसको भी ‘उम्मा’ के शब्द से याद किया जाता है। पवित्र क़ुरआन में यह शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। चुनाँचे इरशाद है “नहीं, बल्कि वे कहते हैं— हमने तो अपने बाप-दादा को एक तरीक़े (उम्मत) पर पाया है और हम उन्हीं के पदचिह्नों पर हैं।” (क़ुरआन, 43:22) बहुदेववादियों और अधर्मियों को जब विभिन्न पैग़म्बरों ने दावत दी और दीन (इस्लाम) की शिक्षा उनके सामने रखी तो उन्होंने इस शिक्षा को अपनी क़ौमी व्यवस्था, रिवाज और बाप-दादा के तरीक़े और दस्तूर के ख़िलाफ़ पाया, इसलिए उसको स्वीकार करने में संकोच किया। उनके इस संकोच को बयान करते हुए पवित्र क़ुरआन ने यह वाक्य नक़्ल किया है। यहाँ ‘उम्मत’ का शब्द इसी प्राचीन परम्परा और व्यवस्था के लिए प्रयोग हुआ है जिसपर कार्यरत रहने का अधर्मी और बहुदेववादी इरादा ज़ाहिर करते थे। ‘उम्मत’ का एक और अर्थ मुद्दत और ज़माना भी है। पवित्र क़ुरआन में यह शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। चुनाँचे एक जगह आता है, हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के वृत्तान्त में कहा गया है “और यूसुफ़ के जेल के एक साथी को एक मुद्दत (उम्मत) के बाद याद आया कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) स्वप्नफल बताने की क्षमता रखते हैं।” इसी तरह से एक और आयत में कहा गया है “अगर हम इन मुजरिमों की सज़ा को एक निर्धारित अवधि (उम्मत) के लिए स्थगित भी कर दें....” (क़ुरआन, 11:8) यहाँ भी ‘उम्मत’ का अर्थ निर्धारित अवधि और ज़माने का है। यहाँ यह इशारा भी अभीष्ट मालूम होता है कि यह ‘उम्मत’ जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने क़ायम की इसको एक सीमित अवधि दी गई है। एक अन्तराल दिया गया है जिसमें यह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की पाबन्द है। यह अन्तराल या अवधि कोई असीमित नहीं है, बल्कि इसका एक निर्धारित समय है जिसके बाद सवाल-जवाब की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
‘उम्मत’ के इन सारे अर्थों को सामने रखते हुए ‘उम्मत’ की विशिष्टताओं का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा पवित्र क़ुरआन और हदीसों में जगह-जगह ‘उम्मत’ की विशिष्टताओं और विशेष गुणों को विभिन्न ढंग और विभिन्न शब्दों में बयान किया गया है। ‘उम्मत’ के विशेष गुणों में सबसे नुमायाँ गुण ‘उम्मत’ (मुस्लिम समुदाय) की एकता है। पवित्र क़ुरआन में ‘उम्मत’ की एकता के विषय को कई जगह अत्यन्त स्पष्ट और दोटूक ढंग से बयान किया गया है। चुनाँचे दो-तीन जगह यह चर्चा आई है “निस्सन्देह यह तुम्हारी ‘उम्मत’ एक मात्र और एकजुट ‘उम्मत’ है।” (क़ुरआन, 23:52) “और मैं तुम्हारा रब हूँ अत: मेरी ही इबादत करो।” (क़ुरआन, 21:92) जिस तरह अल्लाह तआला का एकत्व एक वास्तविकता है इसी तरह ‘उम्मत’ की एकता भी एक वास्तविकता के तौर पर ईमानवालों के सामने रहनी चाहिए। अगर इस सृष्टि का पालनहार एक है। अगर इस ‘उम्मत’ का पैग़म्बर और रसूल एक है। अगर किताब एक है, मंज़िले-मक़्सूद और लक्ष्य एक है, शरीअत और जीवन-व्यवस्था एक है तो फिर ‘उम्मत’ को भी एक एकजुट मुस्लिम समुदाय ही होना बनना, और रहना चाहिए।
‘उम्मत’ की एकता के तीन बड़ी निशानियाँ हैं। एक वाणी की एकता है, दूसरी विचारों की एकता है, तीसरी चरित्र एवं आचरण की एकता है। वाणी की एकता तो मात्र एक लक्षण और शीर्षक है जो यह बताने के लिए है कि ‘उम्मत’ में विचारों की एकता और चरित्र की एकता दोनों मौजूद हैं। अस्ल मक़सद चरित्र की एकता तथा विचारों की एकता की प्राप्ति है। अगर विचारों एवं चरित्र में एकता पाई जाती है तो गोया ‘उम्मत’ अपनी अस्ल पर, एकता और एकजुटता पर क़ायम है। विचारों की एकता का अर्थ यह है कि मुस्लिम समाज पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल में बयान किए गए सिद्धान्तों एवं नियमों पर एकमत हो, मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग अपने लक्ष्य और मंज़िले-मक़्सूद के बारे में सन्तुष्ट हों, जिस रास्ते पर उनको चलना है, जिस मंज़िले-मक़्सूद की तरफ़ सफ़र करके जाना है, उसके मूल गुणों के बारे में सर्वसहमति पाई जाती हो, चरित्र में समानता पाई जाती हो, रवैये में समानता पाई जाती हो, यह चरित्र की एकता है। विचारों की एकता के अर्थ में जो बात बहुत महत्त्वपूर्ण है वह है कि इस सृष्टि के तथ्यों के बारे में मुस्लिम समाज का दृष्टिकोण समष्टीय रूप से एक होना चाहिए। दीनी या धार्मिक लक्ष्य के बारे में उसका दृष्टिकोण एक हो। जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ इंसानियत को समय-समय पर पेश आती रहती हैं उनके बारे में मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया और रवैया क्या होना चाहिए। उसके बारे में सार्वजनिक रूप से मतैक्य पाया जाता हो। छोटे-छोटे आंशिक मामलों या विस्तृत विवरणों में मतभेद और विविधता का अस्तित्व विचारों की एकता के विरुद्ध नहीं है। इसी तरह से रवैये में थोड़ा-बहुत अन्तर, हालात और ज़माने को देखते हुए आंशिक मामलों में फेर-बदल चरित्र की एकता के विरुद्ध नहीं है। विचारों की एकता और चरित्र की एकता का उदाहरण वृक्ष की उस जड़ जैसा है जो तमाम शाखाओं को एक तने से जोड़े रखती है। जिस तरह शाखाओं की मोटाई में, शाखाओं में, पत्तों की संख्या में फूलों के प्रकार में अन्तर हो सकता है, लेकिन इससे वृक्ष की एकता पर असर नहीं पड़ता, इसी तरह विचारों की एकता और चरित्र की एकता का मामला है। विस्तृत विवरण में, आंशिक मामलों में अन्तर हर ज़माने में रहा है और जब तक इंसान मौजूद है, हर इंसान के ख़यालात और विचारों में विविधता और नवीनता पैदा होगी। लेकिन यह विविधता और नवीनता सीमाओं की पाबन्द होनी चाहिए। नियमों और अनुशासन से बंधी होनी चाहिए। वे नियम एवं सिद्धान्त जो पवित्र क़ुरआन में बयान हुए हैं, वे नियम एवं सिद्धान्त जिनपर मुस्लिम समाज का मतैक्य रहा है। इस मतैक्य से जुड़े रहते हुए शरीअत की सीमाओं के अन्दर अगर कोई मतभेद और विविधता है तो वह न केवल गवारा है, बल्कि पसन्दीदा है। स्वीकार्य ही नहीं, बल्कि दरकार है, इसलिए कि इससे विचारों में विविधता पैदा होती है। इंसानी सोच में व्यापकता पैदा होती है। ज्ञान-विज्ञान में विविधता और विकास पैदा होता है।
इन तमाम मामलों का ज़ाहिरी शीर्षक और निशानी वाणी की एकता है। अगर वाणी की एकता को ही पर्याप्त समझ लिया जाए और इसके नतीजे में चरित्र की एकता और विचारों की एकता पैदा न हो तो यह अच्छा संकेत नहीं है। दिल और ज़बान में समरसता होनी चाहिए। जो ज़बान पर है, वह दिलों में होना चाहिए, जो दिलों में है वह ज़बान पर होना चाहिए, और जो ज़बान और दिल दोनों में है उसका इज़हार इंसान के व्यवहार से होना चाहिए। इन तीनों प्रकार की एकताओं के दरमियान भी एकता दरकार है। न केवल मुस्लिम समाज के दरमियान एकता होनी चाहिए, बल्कि एकता की इन तीनों क़िस्मों यानी विचारों की एकता, चरित्र की एकता और वाणी की एकता के दरमियान भी एकता और समरसता दरकार है। ‘उम्मत’ (मुस्लिम समाज) की तीसरी बड़ी विशेषता, सार्वभौमिकता है, यह एक विश्वव्यापी मुस्लिम समुदाय है इस दृष्टि से इसका सम्बन्ध किसी इलाक़े से या रंग से या नस्ल से या ज़बान से नहीं है, बल्कि यह पहले दिन से अरब और उसके बाहर हर जगह के लिए है। पहले दिन से इसमें बिलाल हब्शी जैसे हब्शी भी शामिल थे। सुहैब रूमी जैसे सुर्ख़ चेहरेवाले भी शामिल थे। अरब और ग़ैर-अरब दोनों के लोग इस ‘उम्मत’ में शामिल रहे हैं, और हर दौर में, हर ज़माने और हर इलाक़े में इस ‘उम्मत’ की उमूमी शान और निशानी सार्वभौमिकता रही है।
यह ‘उम्मत’ एक आध्यात्मिक ‘उम्मत’ है। आध्यात्मिकता इसका तीसरा महत्त्वपूर्ण गुण है। आध्यात्मिकता से तात्पर्य यह है कि यह ‘उम्मत’ किसी ज़ाहिरी या भौतिक आधार पर क़ायम नहीं है, बल्कि यह एक अक़ीदे के आधार पर क़ायम है। एक आध्यात्मिक केन्द्र से सम्बद्धता के आधार पर क़ायम है, इसलिए इसका आधार, इसका केन्द्र आध्यात्मिक है, वह मूल विचार इस्लाम का अक़ीदा है, जो लोग इस अक़ीदे से जुड़े होंगे वे इस ‘उम्मत’ के लोग समझे जाएँगे, जो इस अक़ीदे से सम्बद्ध नहीं रहेंगे या नहीं हुए होंगे वे इस ‘उम्मत’ से बाहर होंगे।
‘उम्मत’ की चौथी मौलिक विशेषता समता है। पवित्र क़ुरआन ने मुस्लिम समुदाय के तमाम लोगों को एक-दूसरे का भाई-बहन क़रार दिया है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अगर सब एक-दूसरे के भाई हैं तो भाई-चारे की अपेक्षा समता है। यह नहीं हो सकता कि एक घर में चार भाई रहते हों और चारों बराबर न हों। माँ-बाप की नज़र में सबकी हैसियत बराबर न हो। अगर एक की हैसियत ज़्यादा और दूसरे की कम है तो यह भाई-चारे की अपेक्षा के ख़िलाफ़ है। ऐसा भेदभाव भाई-चारे की धारणा के विरुद्ध है। फिर भाई-चारे की अपेक्षा समता है, समता और भाई-चारा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। समता की अपेक्षा यह है कि मुस्लिम समुदाय में ‘अद्ल’ (न्याय) हो। यह मुस्लिम समुदाय न्याय का ध्वजावाहक हो। अगर समता के सिद्धान्त को मान लिया जाए तो न्याय के सिद्धान्त को भी अवश्य मानना पड़ेगा। इसलिए कि समता की अपेक्षा यह है कि क़ानूनी और नैतिक दृष्टि से, शरई दृष्टि से सब के अधिकार बराबर हों, सबकी ज़िम्मेदारियाँ बराबर हों और क़ानून की नज़र में बतौर शहरी के, बतौर एक ज़िम्मेदार मुसलमान व्यक्ति के, सब बराबर समझे जाएँ और सबके साथ एक ही क़ानून के तहत बरताव किया जाए।
पवित्र क़ुरआन में न्याय और इंसाफ़ पर जगह-जगह और विभिन्न ढंग से ज़ोर दिया गया है और न्याय के विभिन्न पहलुओं को बयान किया गया है। विशेष रूप से उन मामलों का ज़िक्र ज़ोर देकर किया गया है जहाँ इंसान ‘अद्ल’ (न्याय) का दामन हाथ से छोड़ सकता है। इंसान का आम स्वभाव यह है कि वह ‘अद्ल’ का दामन अत्यन्त दुश्मनी या अत्यन्त मुहब्बत में छोड़ता है। जिससे अत्यन्त मुहब्बत हो उसके बारे में न्यायोचित रवैये का ध्यान नहीं रखता, जिसके बारे में सख़्त दुश्मनी का रवैया हो उसके बारे में न्याय और इंसाफ़ का रवैया क़ायम नहीं रहता। पवित्र क़ुरआन ने दोनों पहलुओं का ज़िक्र बहुत मनोयोग से किया है। एक जगह ‘अद्ल’ का आदेश देते हुए कहा कि “अगर तुम्हारा क़रीबी रिश्तेदार भी हो तो भी” (क़ुरआन, 6:152) उसके बारे में ‘अद्ल’ का रवैया अपनाओ। यह न हो कि उससे सम्बन्ध और प्रेम की वजह से दूसरों का अधिकार हनन हो जाए। न्याय और सन्तुलन का दामन हाथ से छूट जाए। इसी तरह से दुश्मनी के बारे में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति या गिरोह से सख़्त दुश्मनी की वजह से न्याय की माँगे प्रभावित हो जाती हैं। “किसी क़ौम की दुश्मनी या किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें हरगिज़ इस बात पर मजबूर न करे कि तुम ‘अद्ल’ (न्याय) का दामन हाथ से छोड़ दो।” (क़ुरआन, 5:8)
‘उम्मत’ की एक और विशेषता यह है कि यह ‘उम्मत’ ज्ञान के आधार पर क़ायम है, बल्कि आजकल तो कहना चाहिए कि ज्ञान के आधार पर क़ायम हुई थी। ज्ञान के आधार से अभिप्रेत यह है कि यह ‘उम्मत’ वह एक मात्र ‘उम्मत’ है जिसको एक शैक्षिक ज़िम्मेदारी दी गई, जिसकी ज़िम्मेदारियों में ज्ञान का प्रचार-प्रसार और शिक्षा का प्रबन्ध भी शामिल है। अतीत में या वर्तमान में कोई ऐसी क़ौम या ‘उम्मत’ इतिहास में नहीं मिलती जिसका मौलिक लक्ष्य और मौलिक पद ज्ञान का प्रचार-प्रसार हो। जिसको शिक्षक के रूप में उठाया गया हो, जिसके पहले पेशवा ने अपने को मूल रूप से शिक्षक (मुअल्लिम) क़रार दिया हो। “मुझे तो केवल मुअल्लिम के तौर पर भेजा गया है।” (हदीस) अगर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मौलिक हैसियत इस सृष्टि और इंसानियत के शिक्षक की थी और ‘उम्मत’ उनके उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रही है तो फिर उस ‘उम्मत’ को भी क़ौमों की शिक्षक और इंसानियत की शिक्षक होना चाहिए।
ज्ञान और न्याय ये दो वे महत्त्वपूर्ण आधार हैं जिनपर मुस्लिम समाज क़ायम है। जिनके आधार पर मुस्लिम समाज अस्तित्व में आया है। जिनके आधार पर इस्लामी सभ्यता ने जन्म लिया। अगर इस्लामी सभ्यता या मुस्लिम समाज के विश्वव्यापी चरित्र को दो महत्त्वपूर्ण शीर्षकों के तहत बयान किया जाए तो वे महत्त्वपूर्ण शीर्षक ज्ञान और न्याय ही होंगे। ज्ञान और इंसाफ़ के साथ-साथ मुस्लिम समाज को ‘बिर्र’ का आदेश भी दिया गया है। ‘बिर्र’ पवित्र क़ुरआन की एक शब्दावली है जिसमें भलाई, नेकी और सद्व्यवहार की हर क़िस्म शामिल है। अच्छाई और भलाई की जितनी क़िस्में हो सकती हैं वे इंसानियत की भलाई की हों, वे मुसलमानों की भलाई की हों, वे इस सृष्टि की भलाई की हों, यहाँ तक कि पशु-पक्षी और वनस्पति जगत् की भलाई से सम्बन्ध रखती हों, वे सब ‘बिर्र’ में शामिल हैं।
पवित्र क़ुरआन में एक जगह ‘बिर्र’ के बहुत-से महत्त्वपूर्ण पहलुओं को बयान करते हुए कहा गया कि ‘बिर्र’ मात्र यही नहीं है कि तुम एक ख़ास तरफ़ मुँह करके इबादत करो, बल्कि ‘बिर्र’ में जो बातें शामिल हैं, वे अल्लाह पर ईमान, आख़िरत यानी परलोक पर ईमान, किताबों पर ईमान, पैग़म्बरों पर ईमान, मिस्कीनों को खाना खिलाना, रिश्तेदारों के अधिकारों का ध्यान रखना, यतीमों की भलाई का प्रबन्ध करना, ये सारे मामलात जिसमें पूरी इंसानियत की भलाई शामिल है, ये सब ‘बिर्र’ में शामिल हैं। आज पश्चिमी जगत् में उदारता की शब्दावली की बड़ी चर्चा है। वे समझते हैं कि tolerance यानी उदारता के रवैये को अपनाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा सिद्धान्त दुनिया को दे दिया है। मालूम नहीं वे कितने उदार हैं या कितने नहीं हैं, मुसलमानों का अनुभव तो उनकी उदारता के बारे में उत्साहित करनेवाला नहीं है। लेकिन उदारता के बारे में अगर इन सारे दावों और धारणाओं को मान भी लिया जाए जो पश्चिमी दुनिया में किताबों में लिखी जाती हैं और जिनसे लेखों और भाषणों को सजाया जाता है, उनको स्वीकार भी कर लिया जाए तो सच यह है कि ‘बिर्र’ का दर्जा उदारता के दर्जे से बहुत ऊँचा है। उदारता के शब्द में यह बात शामिल है कि आप एक व्यक्ति को वास्तव में ना-पसन्द करते हैं, एक व्यक्ति से दिल से नफ़रत करते हैं लेकिन उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहनशीलता, बर्दाश्त, और tolerance से यही अर्थ निकलता है। आप उसको Tolerate कर रहे हैं, यह एक दृष्टि से नकारात्मक प्रकार का रवैया है, लेकिन इसके विपरीत ‘बिर्र’ एक बहुत सकारात्मक रवैया है, ‘बिर्र’ सकारात्मक रूप से इंसानों की सेवा, ग़रीबों और दरिद्रों की सहायता और मुहताजों के साथ सद्व्यवहार का रवैया है। ‘उम्मत’ को ‘बिर्र’ का आदेश दिया गया है जो उदारता से बहुत ऊँचे दर्जे की चीज़ है।
‘उम्मत’ के चरित्र में एक और महत्त्वपूर्ण पहलू दिल को मोहने का रवैया है। दिल को मोहना भी इस्लाम के दूसरों से अलग होने का एक सुबूत है। दिल को मोहने का अर्थ यह है कि विरोधी या दुश्मन या अजनबी के साथ ऐसा सुलूक किया जाए, ऐसा रवैया और तरीक़ा अपनाया जाए कि आप उसके दिल को जीतने में कामयाब हो जाएँ। इंसान के जिस्म पर क़ाबू पाना आसान है, इंसान के जिस्म पर विजय पा लेना मुश्किल नहीं है। हर ताक़तवर इंसान कमज़ोर इंसान के जिस्म पर विजय पा सकता है। लेकिन इंसानों के दिलों को जीतना बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम की दिलचपसी लोगों के जिस्म पर हुकूमत करने से नहीं है, इस्लाम की दिलचस्पी लोगों के दिलों को जीतने से है। अतीत में पहले दिन से लेकर आज तक जो लोग इस्लाम में दाख़िल हुए हैं उनमें अति प्रभावी निन्यानवे प्रतिशत से भी बढ़कर संख्या उन लोगों की है जो इस्लाम की शिक्षाओं की ख़ूबी और कुछ मुसलमानों के सदाचरण को देखकर मुसलमान हुए। इस्लाम के मुख्य दौर में हर मुसलमान का शिष्टाचार ऐसा था कि ग़ैर-मुस्लिम उसको देखकर मुसलमान होता था। समय के साथ-साथ ऐसे मुसलमानों की संख्या कम होती गई जिनका शिष्टाचार लोगों के लिए ध्यानाकर्षण का कारण था, जिनका चरित्र दूसरों के लिए इस्लाम स्वीकार करने का कारण बना। आज ऐसे मुसलमान बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर एक मुसलमान भी कहीं ऐसा है जिसका नैतिक आचरण इस्लाम का नमूना या झलक है, आज भी उसको देखकर हज़ारों लोग इस्लाम की तरफ़ माइल होते हैं।
तालीफ़े-क़ल्ब (दिलों को नर्म कर लेना) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िन्दगी के मौलिक गुणों में से एक गुण है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जंगों में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, समझौतों में, क़बीलों और हुकूमतों से लेन-देन में दिलों को जीतने के सिद्धान्त को आजकल के ज़माने की भाषा में हम कह सकते हैं कि अपनी विदेश नीति का एक मौलिक सिद्धान्त क़रार दिया। दिलों को जीतने का इससे बढ़कर और क्या महत्त्व होगा कि इस्लाम में चार मौलिक इबादतों में से, चार स्तम्भों में से एक, यानी ज़कात की महत्त्वपूर्ण मदों में से एक मद तालीफ़े-क़ल्ब (दिलों के जीतने) को भी क़रार दिया, यानी ज़कात जो मुसलमान के लिए इबादत का दर्जा रखती है, इस्लाम के चार बड़े स्तम्भों में से एक स्तम्भ है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धता और धन की शुद्धता है, इस रक़म को जहाँ-जहाँ ख़र्च करने का आदेश दिया गया है वहाँ एक मद ग़ैर-मुस्लिम दुश्मनों का दिल जीतना भी है। अगर ज़कात की रक़म से इस्लाम-दुश्मन व्यक्तित्वों को या गिरोहों को इस तरह से क़रीब लाया जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, उनमें से अगर कोई बीमार हो तो उसका इलाज करने में यह रक़म ख़र्च की जाए, उनमें से अगर कोई मुहताज हो तो उसकी मोहताजी दूर करने में इस रक़म से फ़ायदा उठाया जाए, ताकि उसके दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वह दूर हो जाए और वह इस्लाम के क़रीब आ जाए।
तालीफ़े-क़ल्ब (दिलों को मोहने) से एक और सिद्धान्त की निशानदेही होती है और वह नैतिकता है। इस्लाम का सर्वप्रथम और सबसे आख़िरी माध्यम इस्लाम के प्रसार के लिए नैतिक रवैया और नैतिक मूल्यों की पैरवी है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक जगह फ़रमाया कि “मुझे तो केवल उच्च नैतिकता की पूर्ति के लिए भेजा गया है।” गोया दो मौलिक लक्ष्य उन्होंने क़रार दिए। एक सारे जगत् की शिक्षा, मानवता की शिक्षा और एक उच्च नैतिकता की पूर्ति। उच्च नैतिकता का अर्थ यह है कि मुसलमान का नैतिक रवैया हर व्यक्ति के बारे में ऐसा हो कि दूसरे का स्वभाव, उसका दिल, और उसकी आत्मा इस बात की गवाही दें कि अगर नैतिकता का कोई पैमाना है तो यह है। अगर नैतिकता का कोई मापदंड है तो यह है।
इस्लामी शिष्टाचार में जो शिष्टता सबसे नुमायाँ होनी चाहिए जिसकी तरफ़ हदीसों में भी इशारा किया गया है वह ‘हया’ है। हया यानी नज़र की पाकीज़गी, ख़याल की पाकीज़गी, इरादे और संकल्प की पवित्रता और इंसानों से सम्बन्ध में सफ़ाई-सुथराई, ये सब हया ही की मौलिक निशानियाँ हैं। इस्लामी समाज में सम्बन्धों का आधार, नैतिकता और हया के सिद्धान्त हैं, परिवार का गठन इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर होता है। इंसानों के दरमियान मामलों और लेन-देन की मूल आत्मा यही है। एक पश्चिमी विद्वान ने बहुत अच्छा लिखा है। उसने कहा है कि इस्लामी शरीअत वस्तुतः नैतिकता की धारणाओं को क़ानूनी रूप से लागू करने का एक सफल प्रयास है। गोया शरीअत ने नैतिकता एवं क़ानून को इकट्ठा कर दिया है। क़ानून और नैतिकता के अलग होने से जो समस्याएँ पैदा हुई हैं उनसे पश्चिमी दुनिया आज पीछा छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस्लामी शरीअत ने पहले दिन से यह रास्ता बन्द कर दिया था कि नैतिकता और क़ानून को एक-दूसरे से अलग-अलग करके देखा जाए। जब तक नैतिकता और क़ानून एक जगह रहेंगे, उस समय तक जनसाधारण वे तमाम लाभ प्राप्त करते रहेंगे जो वे क़ानून और नैतिकता से प्राप्त करना चाहते हैं। जिस लम्हे ये दोनों अलग-अलग हो गए उस लम्हे क़ानून की उपयोगिता भी कमज़ोर पड़ जाती है और नैतिकता भी अपना असर खो बैठती है।
मुस्लिम समाज का एक महत्त्वपूर्ण चरित्र जो पवित्र क़ुरआन में बयान किया गया है वह ‘शहादत अलन-नास’ (लोगों पर गवाही देना) है। ‘शहादत अलन-नास’ पवित्र क़ुरआन के अनुसार ‘उम्मते-वसत’ (उत्तम समुदाय) होने की अनिवार्य अपेक्षा है। “हमने तुम्हें एक उत्तम समुदाय इसी लिए बनाया है कि तुम लोगों के मुक़ाबले में, इंसानियत के मुक़ाबले में सत्य के गवाह और अल्लाह के दीन के गवाह बनो और पैग़म्बर तुम्हारे बारे में गवाह बनें।” (क़ुरआन, 2:143) यानी जो ज़िम्मेदारी, जो चरित्र और जो रवैया पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) का तुम्हारे बारे में है वही रवैया और चरित्र पूरी मानवता के बारे में तुम्हारा होना चाहिए। यही वह बात है जिसको एक दूसरे सन्दर्भ में एक दूसरी आयत में ‘उख़रिजत लिन्नास’ के शब्दों से याद किया गया। “तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसको इंसानों के फ़ायदे के लिए निकाला गया है।” (क़ुरआन, 3:110) इंसानों के फ़ायदे के लिए भेजा गया है। यहाँ ‘उख़रिज’ का शब्द बड़ा महत्त्वपूर्ण है, यह ‘उम्मत’ निकाली गई है जिस तरह से किसी व्यक्ति को किसी ज़िम्मेदारी के लिए भेजा जाता है तो अपने घर से या वर्तमान कार्यक्षेत्र से निकालकर दूसरी जगह रवाना कर दिया जाता है, वही कैफ़ियत या उपमा इस उम्मत की भी है कि इसको पूरी इंसानियत के लाभ के लिए एक मुहिम पर निकाला गया है। अत: पूरा मुस्लिम समाज इस मुहिम पर निकला हुआ है। यह बात अनेक हदीसों में भी बयान हुई है। उन तमाम हदीसों को एक चर्चा में बयान करना मुश्किल है, लेकिन अनेक हदीसों में जगह-जगह ‘उम्मते-वसत’ (उत्तम समुदाय) होने के विभिन्न पहलुओं को, ‘उम्मते-वसत’ होने की विभिन्न अपेक्षाओं को, और ‘उम्मते-वसत’ होने की विभिन्न ज़िम्मेदारियों को विभिन्न शैलियों में बयान किया गया है। एक जगह मुसनदे-इमाम अहमद की रिवायत में कहा गया है कि “तुम एक ऐसी ‘उम्मत’ हो जिसके द्वारा अल्लाह तआला ने इंसानों के लिए आसानी पैदा करने का इरादा किया है।” ‘युस्र’ को तुम्हारे द्वारा आम किया गया है। तुम इंसानियत की समस्याओं को ख़त्म करके आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो। इंसानों की अनावश्यक मुश्किलों को दूर करके उनके लिए आसानियाँ पैदा करना तुम्हारी मौलिक ज़िम्मेदारी है।
यह है वह मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम समाज जिसको पवित्र क़ुरआन के अनुसार इस्लाम की पहली सामूहिक ज़िम्मेदारी क़रार दिया जा सकता है। यह विश्व के मुसलमानों की सर्वप्रथम सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे अपने-आपको एक विश्वव्यापी आदर्श मुस्लिम समाज के रूप में गठित करें। यह ‘उम्मत’ या समाज या विश्वव्यापी समाज जहाँ शरीअत की व्यवस्था और शरीअत की शिक्षा का ध्वजावाहक है और जिसमें वे विशिष्टताएँ इकट्ठी हो गई हैं जो इस्लामी शरीअत के बारे में बयान की जा चुकी हैं, वहाँ यह चार मौलिक गुणों से भी विभूषित है। ये चार मौलिक गुण वे हैं जिनमें मुस्लिम समाज की सारी विशिष्टताएँ एकत्र हो जाती हैं। ये विशिष्टताएँ तो अनगिनत हैं। जिनमें से कुछ का उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया जा चुका है।
लेकिन अगर इन तमाम विशिष्टताओं को और उन तमाम मौलिक गुणों को चार शीर्षकों के अन्तर्गत बयान किया जाए तो वे चार शीर्षक होंगे। ज्ञान, न्याय, समता और नैतिकता। मुस्लिम समाज की बुनियाद न्याय पर है, ज्ञान पर है, समता और नैतिकता पर है। जहालत और अज्ञानता के साथ मुस्लिम समाज के दायित्व पूरे नहीं किए जा सकते। न्याय के बिना ‘उम्मत’ इस आधार पर क़ायम नहीं रह सकती जिस आधार पर इसको क़ायम रहना चाहिए। समता के बिना मुस्लिम समाज में एकता और सौहार्द क़ायम नहीं रह सकता। नैतिकता के बिना मुस्लिम समाज की कथनी और करनी में वह समरूपता पैदा नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। इन चार विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता ज्ञान और शिक्षा है। अगर पूरी इंसानियत के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग वह जहाँ इंसानों के मामलों का आधार ज्ञान के बजाय अन्य प्रवृत्तियाँ हैं और दूसरा दौर वह जहाँ इंसानी मामलों का आधार ज्ञान और बुद्धि और तत्त्वदर्शिता हैं, यह विभाजन बहुत आसानी से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शुभ जन्म और पवित्र क़ुरआन के अवतरण के आधार पर क़रार दिया जा सकता है। पवित्र क़ुरआन के अवतरण से पहले का ज़माना ज्ञान और तत्त्वदर्शिता से दूरी तथा बुद्धि विरोधी व्यवस्था बनाने का दौर है।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया में आने के बाद और पवित्र क़ुरआन के अवतरण के बाद का दौर क्रमशः ज्ञान के फैलने का, तत्त्वदर्शिता के फैलाव का, और बुद्धि की भूमिका में वृद्धि का दौर है। इस्लाम ने ज्ञान को भी बयान किया और ज्ञान की वास्तविकता को भी बयान किया, इस्लामी समाज ने शिष्य और शिक्षक को उच्चतम स्थान पर आसीन किया, इस्लामी समाज में पाठशाला और किताब को अत्यन्त महत्त्व प्राप्त हुआ। इस्लामी समाज ने काग़ज़ और क़लम को महत्व दिया। विद्या और विद्वान को नेतृत्व के स्थान पर आसीन किया। इस्लामी समाज ने मानवता को नए-नए ज्ञान-विज्ञान प्रदान किए, ज्ञान-विज्ञान के मामले में मुसलमान विद्वानों ने नई-नई प्रवृत्तियाँ इंसानियत के सामने पेश कीं और ज्ञान-विज्ञान को इतना विकास दिया कि उनकी संख्या सैंकड़ों से बढ़ाकर हज़ारों तक पहुँचा दी। प्राचीन तथा आधुनिक काल में जितनी विधाएँ पाई जाती हैं उन सबका आधार, उन सबकी जड़ इस्लामी शरीअत और इस्लामी सभ्यता की नींव में मौजूद है।
पवित्र क़ुरआन ने जिस शरीअत की शिक्षा दी है उसके मौलिक उद्देश्यों में बुद्धि की रक्षा एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है, शरीअत के पाँच उद्देश्यों में बुद्धि की रक्षा अति महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इसलिए कि अल्लाह की शरीअत ने इंसान को एक सामर्थ्यवान इंसान बनाया है, एक सामर्थ्यवान प्राणी क़रार दिया है, ऐसा प्राणी जिसको समझ और बुद्धि की दौलत प्रदान की गई है, ऐसा प्राणी जिसको सृष्टि की बड़ी-बड़ी रचनाओं पर वरीयता दी गई है। ऐसा प्राणी जिसको यह ज़िम्मेदारी प्रदान की गई, जिसको उठाने से ज़मीनों ने, आसमानों ने, और पहाड़ों जैसी बड़ी-बड़ी स्रष्ट रचनाओं ने हाथ जोड़ लिए थे, इंसान ने उसको उठा लिया इसलिए कि इंसान के पास बुद्धि थी, इंसान के पास इरादा था, इंसान को आज़ादी दी गई थी और इंसान एक ज़िम्मेदार प्राणी था। इस बुद्धि और ज़िम्मेदारी और अमानत का भार सहने की सबसे मौलिक शर्त ज्ञान की चाहत है, पढ़ाई-लिखाई है, नबी ‘उम्मी’ पर जो सबसे पहली वह्य (ईश-प्रकाशना) अवतरित हुई वह ‘इक़रा’ थी। गोया पवित्र क़ुरआन का आरम्भ ‘पढ़ो’ के शीर्षक से एक नए दौर का प्रतिनिधि और एक नए ज़माने को ज़ाहिर करनेवाला है। यही वजह है कि ज्ञान की प्राप्ति को हर मुसलमान पुरुष और स्त्री का कर्त्तव्य क़रार दिया गया। बताया गया कि विद्वान और अशिक्षित बाराबर नहीं हो सकते। आदेश दिया गया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी उम्र या किसी समय की क़ैद नहीं है। पालने से लेकर क़ब्र तक ज्ञान की प्राप्ति जारी रहनी चाहिए। इस्लामी विद्वानों की ज़िन्दगी में ऐसी सैंकड़ों मिसालें मिलती हैं कि एक समय के आलिम ने चाहे वे शरीअत के विद्वान हों, वे चिकित्सा के विद्वान हों, वे विज्ञान और गणित के विद्वान हों, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि मृत्यु-शय्या पर अन्तिम साँसों में उनके दिल-दिमाग़ इल्मी समस्याओं और इल्मी गुत्थियों को सुलझाने में व्यस्थ थे। गोया उन्होंने अपनी ज़िन्दगी से व्यवहारतः यह साबित कर दिया कि ज्ञान की प्राप्ति पालने से लेकर क़ब्र तक होती है। बुद्धि की रक्षा का सम्बन्ध जहाँ ज्ञान-विज्ञान से है वहाँ इस्लामी सभ्यता एवं संस्कृति से भी है। इसलिए कि इस्लामी सभ्यता का आधार बुद्धि तथा चिन्तन पर है, अन्धविश्वासों और फ़ालतू रस्मों पर नहीं है। पवित्र क़ुरआन वह एकमात्र आसमानी किताब है जिसने ‘जिब्त’ और ‘ताग़ूत’ यानी ख़ुराफ़ात और बे-बुनियाद बातों को, अबौद्धिक बातों को कुफ़्र (अधर्म) के बराबर समझा है और उनका इनकार करने का आदेश दिया है।
इस्लामी विद्वानों ने पवित्र क़ुरआन और हदीसों की बुनियाद पर ज्ञान प्राप्त करने के बहुत-से दर्जे बताए हैं। इन दर्जों का विवरण पिछले एक लेक्चर में बताया जा चुका है। इन दर्जों में से एक दर्जा फ़र्ज़े-ऐन का है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, एक दर्जा फ़र्ज़े-किफ़ाया का है जो मुस्लिम समाज के ज़िम्मे समष्टीय रूप से अनिवार्य है, बशर्तेकि कुछ लोग प्रभावकारी रूप से इस फ़र्ज़ को अंजाम दें। एक दर्जा वह है जो फ़र्ज़े-किफ़ाया का भी फ़र्ज़े-किफ़ाया है, यानी वे प्रतिष्ठित उलमा या विद्वान लोग जो मुस्लिम समुदाय की तरफ़ से इस फ़र्ज़े-किफ़ाया को अंजाम देंगे। उनपर समष्टीय रूप से फ़र्ज़े-किफ़ाया की ज़िम्मेदारी आती है कि उनमें एक सीमित संख्या ऐसे महान विद्वानों की, पहली पंक्ति के इस्लामी चिन्तकों की, उच्च कोटि के मुज्तहिदीन (इज्तिहाद करनेवालों) की मौजूद हो जो नए मामलों मैं ख़ुद उलमा और विद्वानों का मार्गदर्शन कर सकें।
इस्लामी शरीअत ने पहली बार इल्मे-नाफ़े (लाभकारी ज्ञान) और इल्मे-ग़ैर-नाफ़े (अलाभकारी ज्ञान) के दरमियान अन्तर बताया है। उलूम (ज्ञान) के यों तो बहुत-से प्रकार हैं, सृष्टि के तथ्यों की खोज की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सृष्टि के तथ्यों की खोज के वे पहलू तो निश्चय ही लाभकारी हैं जो इंसानों के लिए इस दुनिया या उस दुनिया में लाभकारी हों, लेकिन अगर सृष्टि की खोज, या सृष्टि के रहस्योद्घाटन के कुछ पहलू ऐसे हों कि जो मानवता के लिए इस दुनिया में भी लाभकारी न हों और आख़िरत में भी लाभकारी न हों, तो उनमें समय लगाना समय की भी बर्बादी है और संसाधनों की भी।
ये दर्जा जिसको ज्ञान प्राप्ति में फ़र्ज़े-ऐन कहा गया है यह वह है जो फ़राइज़े-दीन (धर्म के द्वारा लागू होनेवाले कर्त्तव्यों) के निर्वहन के लिए ज़रूरी है। फ़राइज़े-दीन से तीन प्रकार के फ़राइज़ मुराद हैं, सबसे पहले तो वे अक़ीदे (धार्मिक अवधारणाएँ) हैं जिनका सुधार होना चाहिए, जिनपर ईमान लाकर इंसान इस्लाम में दाख़िल होता है, जिनके द्वारा अक़ीदा खड़ा होता है। दूसरा दर्जा उन शिक्षाओं का है जो इंसान को इबादतों के अदा करने का तरीक़ा सिखाता है, हर व्यक्ति पर नमाज़ फ़र्ज़ है, बालिग़ (वयस्क) पर रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर निसाब (एक निश्चित मात्रा) के अनुसार धन हो तो ज़कात फ़र्ज़ है, संसाधन और क्षमता मौजूद हों तो हज फ़र्ज़ है। इन तमाम इबादतों के आदेश जब तक मालूम न हों इन इबादतों को अदा करना सम्भव नहीं है। इसलिए शरीअत के ज्ञाताओं ने इस्लाम के अक़ीदों और इबादतों के ज़रूरी मसाइल (विस्तृत आदेशों) के ज्ञान को फ़र्ज़े-ऐन क़रार दिया।
इस दर्जे के बाद दूसरा दर्जा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है, यह वह दर्जा है जो किसी व्यक्ति के निजी पेशे या ज़िन्दगी से सम्बन्धित हो, एक व्यक्ति व्यापार का काम करता है तो उसको व्यापार के आदेशों का ज्ञान होना चाहिए, एक व्यक्ति कृषि का पेशा अपनाता है तो उसके पास कृषि के आदेशों का ज्ञान होना चाहिए। जिस ज़रिए से इंसान को रोज़ी प्राप्त हो रही है, जिस तरह इंसान ज़िन्दगी गुज़ार रहा है, जिस सरगर्मी से इंसान का सम्बन्ध है, उस सरगर्मी और उस ज़िन्दगी के पहलू के बारे में ज़रूरी ज्ञान इंसान को आना चाहिए। यह ज़रूरी ज्ञान शरीअत का ज्ञान भी होगा और उस मैदान का ज्ञान भी होगा, उस व्यक्ति या उस निपुणता का ज्ञान भी होगा जो इंसान अपनाना चाहता है। शरीअत ने इस बात को जायज़ नहीं रखा कि कोई व्यक्ति चिकित्सा का पेशा अपना ले, इंसानों का इलाज करने की ज़िम्मेदारी ले-ले और वह इस कला को न जानता हो। एक हदीस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने चिकित्सा का पेशा अपना लिया और वह चिकित्सा नहीं जानता था, उसके नतीजे में कोई व्यक्ति किसी मुश्किल का शिकार हो गया, बीमार हो गया, उसकी जान या उसका कोई अंग नष्ट हो गया तो उसकी क़ानूनी ज़िम्मेदारी उस इलाज करनेवाले अयोग्य और नालायक़ डॉक्टर पर होगी, यह उसका ज़ामिन होगा, मर गया तो ‘दियत’ अदा करनी पड़ेगी, कोई अंग नष्ट हो गया तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा और क़ानून में जो फ़ौजदारी ज़िम्मेदारी है वह भी उसपर लागू होगी। इसलिए किसी भी दौर के प्रसिद्ध और प्रचलित मापदंड के अनुसार जो-जो ज्ञान-विज्ञान अनिवार्य हैं वे हर उस इंसान के लिए फ़र्ज़े-ऐन का दर्जा रखते हैं जो उन ज्ञान-विज्ञान को अपनाना चाहे। जो शख़्स अपने-आपको आलिमे-दीन के पद पर आसीन समझता हो, लोगों को फ़तवे देता हो, शरीअत के मामलों में मार्गदर्शन का दावा करता हो, वह अगर शरीअत का ज्ञान नहीं रखता तो उसको इसकी अनुमति नहीं है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ऐसे व्यक्ति को ‘मुफ़्ती-माजन’ के उपनाम से याद किया है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क़रार दी है कि वह ‘मुफ़्ती-माजन’ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ऐसे अयोग्य और अज्ञानी लोगों को दीन के मामलात में राय देने से रोके। इसलिए कि जाहिल लोग ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए यह दर्जा फ़र्ज़े-ऐन है जिसके ये तीन हिस्से मैंने बता दिए हैं, एक वह हिस्सा जिसका सम्बन्ध अक़ीदों से है, दूसरा वह हिस्सा जिसका सम्बन्ध इबादतों के अंजाम देने से है, और तीसरा हिस्सा वह जिसका सम्बन्ध इंसान की रोज़मर्रा ज़िन्दगी से है, रोज़मर्रा ज़िन्दगी में शरीअत के आदेश भी शामिल हैं और सम्बन्धित कला या विशेष योग्यता के आदेश भी।
यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए और इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसको स्पष्ट किया है। इमाम नववी ने उदाहरण के रूप में लिखा है कि जब हम इबादतों के आदेशों को फ़र्ज़े-ऐन क़रार देते हैं या अक़ीदों के ज्ञान को फ़र्ज़े-ऐन क़रार देते हैं तो इससे मुराद वे बड़े-बड़े मौलिक आदेश हैं जिनका ज्ञान हर मुसलमान को होना चाहिए। इससे मुराद वह गूढ़ और सूक्ष्म मामले नहीं हैं जो हर व्यक्ति को पेश नहीं आते और जिनका सम्बन्ध केवल विद्वानों के वर्गों से होता है। विद्वान और शोधकर्ता अपने शोध के आधार पर बहुत-सी नाज़ुक समस्याओं पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये नाज़ुक मामले आम आदमी को प्रायः पेश नहीं आते, इसलिए उनका ज्ञान फ़र्ज़े-किफ़ाया है। फ़र्ज़े-ऐन नहीं है। इमाम नववी ने यह भी लिखा है कि फ़र्ज़े-ऐन का एक दर्जा यह भी है कि क्रय-विक्रय के उमूमी आदेशों का ज्ञान प्राप्त हो, क्रय-विक्रय में क्या चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, यह भी हर व्यक्ति को आना चाहिए। इसलिए कि ये वे मामले हैं जिनकी हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, अब एक व्यक्ति अगर रोटी ख़रीदने बाज़ार जाएगा और उसको क्रय-विक्रय के मौलिक आदेशों का ज्ञान न हो तो हो सकता है कि वह नाजायज़ कार्य का जुर्म कर बैठे, हो सकता है कि वह ‘रिबा’ और ब्याज आधारित व्यापार में लिप्त हो जाए, इसी तरह से जो आध्यात्मिक ख़राबियाँ हैं या आन्तरिक ख़राबियाँ हैं जैसे ईर्ष्या है, दिखावा है, आत्ममुग्धता है, उनकी बुराई भी एक दर्जे में जनसाधारण की जानकारी में होनी चाहिए और यह इस्लामी विद्वानों की ज़िम्मेदारी है कि वे जनसाधारण को इन ख़राबियों से अवगत रखें और उनसे बचने की नसीहत करते रहें।
इस्लाम के इतिहास में और इस्लाम की सभ्यता में ज्ञान को हमेशा एक इकाई समझा गया है ज्ञान को सुविधा की ख़ातिर इल्मे-दीन (धार्मिक ज्ञान) और इल्मे-दुनिया (सांसारिक ज्ञान) में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ज्ञान की वास्तविकता का सम्बन्ध है वह एक ही है और वह इकाई की हैसियत रखता है। शरीअत के ज्ञान में और दुनिया के ज्ञान में कोई टकराव या विरोधाभास नहीं है, अगर टकराव है तो या तो इंसानों से दुनिया के ज्ञान को समझने में ग़लती हुई है और अधिक चिन्तन-मनन की ज़रूरत है या शरीअत के आदेशों को समझने में कहीं ग़लती हुई है।
अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) ने एक बहुत मोटी और सारगर्भित किताब लिखी है जिसका शीर्षक ही यह है ‘दरए तआरुज़ अल-अक़्ल वन-नक़्ल’ कि बुद्धि और पुस्तकीय ज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है, यानी जो ज्ञान-विज्ञान और जो आदेश एवं शिक्षाएँ नक़्ल के द्वारा यानी पवित्र क़ुरआन और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत के द्वारा हम तक पहुँची हैं उनमें और उन शोधों और खोजों में जो इंसानों ने अपनी बुद्धि से स्पष्ट किए हैं कोई टकराव नहीं है, बशर्तेकि जिस चीज़ को बुद्धि की माँग क़रार दिया जा रहा है वह वास्तव में बुद्धिसंगत हो यानी स्पष्ट रूप से बुद्धि के सिद्धान्तों पर साबित होती हो, वह मात्र किसी की राय या मात्र किसी का ख़याल या मात्र किसी की सोच न हो। आज मुस्लिम जगत् में पश्चिम में चलनेवाली हर राय या हर ख़याल को बुद्धि की माँग समझकर बिना ना-नुकुर किए स्वीकार कर लेने का आह्वान किया जाता है। कुछ समय बाद पता चलता है कि यह तो ग़लत बात थी, शोध से ग़लत साबित हुई। यों हर नई आनेवाली बात को खींच-तानकर पवित्र क़ुरआन और सुन्नत की शिक्षा से मिलाने की कोशिश की जाती है। यह रवैया ईमान की कमज़ोरी का और बौद्धिक ग़ुलामी का और वैचारिक बन्दगी की निशानी है। जो चीज़ सहीहुल-मनक़ूल है, यानी उद्धरण के तौर पर पूरी तरह प्रमाणित है जैसे पवित्र क़ुरआन, या प्रमाणित हदीसें और सुन्नते-मुतवातिरा (लगातार चला आ रहा तरीक़ा), इसमें और बुद्धिसंगत में यानी जिसका बौद्धिक माँग होना स्पष्ट साबित हो, जैसे दो और दो चार होते हैं, उनमें और शरीअत के आदेशों में कोई टकराव नहीं है।
जहाँ तक वैज्ञानिकों की और समाज शास्त्रियों के शोध का सम्बन्ध है तो यह समय के साथ-साथ बदलता रहता है, उनमें विकास होता रहता है, उनमें से किसी चीज़ को फ़ाइनल क़रार देकर शरीअत के स्पष्ट आदेशों और स्पष्ट ‘नुसूस’ का मन-माना अर्थ बयान करना और कुछ साल के बाद फिर जब वे विचार यूरोप में बदल जाएँ तो फिर शरीअत के आदेशों को नए सिरे से चिन्तन-मनन का विषय बनाना यह अत्यन्त अनुचित रवैया है। यह रवैया न पैदा हो अगर ज्ञान-विज्ञान की एकता की धारणा ज़िन्दा रहे और पवित्र क़ुरआन और प्रमाणित हदीसों के फ़ाइनल और निश्चित होने पर ईमान पक्का हो। इस्लामी विद्वानों ने ज्ञान की इस एकता को बहुत-सी शैलियों में बयान किया है। किसी ने ‘एहसाए-उलूम’ या ‘तक़सीमाते-उलूम’ के नाम से बयान किया, यों तो अनेक इस्लामी विद्वानों ने ‘तक़सीमे-उलूम’ (ज्ञान का विभाजन) पर किताबें लिखीं, अल-किंदी जो प्रसिद्ध दार्शनिक है, जिसको ‘अरब का दार्शनिक’ कहा जाता है उसने भी इस विषय पर दो किताबें लिखी थीं और भी एक-दो लोगों ने इस विषय पर किताबें लिखीं, लेकिन प्राचीनतम पुस्तक जो बड़ी सारगर्भित और अत्यन्त गूढ़ ढंग से लिखी गई और हम तक पहुँची है, वह प्रसिद्ध मुसलमान दार्शनिक हकीम अबू-नस्र अल-फ़ारॉबी की ‘एहसाउल-उलूम’ है। ‘एहसाउल-उलूम’ के बाद लगभग हर दौर के विद्वानों ने ज्ञान के विभाजन पर काम किया और ज्ञान की एकता की इस्लामी धारणा को विभिन्न पहलुओं से उजागर करने की कोशिश की। यह सिलसिला दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी तक जारी रहा। आख़िरी लेखक जिन्होंने इस कला को चरम तक पहुँचाया, वे हाजी ख़लीफ़ा और अल्लामा अहमद-बिन-मुस्तफ़ा थे जो ताश-कबरीज़ादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस विषय पर बहुत-सी किताबें लिखीं। ताश-कबरीज़ादा के बाद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज्ञान की एकता पर रौशनी डाली और विभिन्न इस्लामी ज्ञान-विज्ञान को एक नए ढंग से बयान किया।
यह तो वह दर्जा था जिसको हम फ़र्ज़े-ऐन कहते हैं। इसके बाद का दर्जा फ़र्ज़े-किफ़ाया है, फ़र्ज़े-किफ़ाया का दर्जा एक दर्जा नहीं है, बल्कि यह समय के साथ-साथ बढ़ता रहता है और इसमें वृद्धि होती रहती है, जैसे-जैसे ज्ञान-विज्ञान फैलते जाएँगे, जैसे-जैसे ज्ञान-विज्ञान में विकास होता जाएगा, उसी तरह से ज्ञान-विज्ञान की व्यापकता भी बढ़ती जाएगी और फ़र्ज़े-किफ़ाया की सतह भी बढ़ती जाएगी। फ़र्ज़े-किफ़ाया के बारे में इस्लामी विद्वानों ने लिखा है कि अगर फ़र्ज़े-किफ़ाया का वास्तविक स्तर प्राप्त न किया जा सके और मुस्लिम समाज में ऐसे लोग मौजूद न रहें जो जनसाधारण का मार्गदर्शन कर सकें और ऐसे लोग न रहें जो इस्लामी विद्वानों का मार्गदर्शन कर सकें तो फिर पूरा मुस्लिम समाज जवाबदेह होगा और उसको गुनाहगार समझा जाएगा। जिन-जिन लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त होता जाए और यह एहसास होता जाए कि इस समय इस सतह के विद्वानों की कमी है, उनकी यह ज़िम्मेदारी है कि वह इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें।
इमाम नववी ने लिखा है “जिस-जिस व्यक्ति को इसका आभास होता जाए कि फ़र्ज़े-किफ़ाया का यह दर्जा छूटा जा रहा है और वह इस कमी को दूर करने का सामर्थ्य रखता हो और वह इसमें कोई हिस्सा ले सकता हो और वह हिस्सा न ले तो वह गुनहगार होगा और इस स्थिति का ज़िम्मेदार समझा जाएगा।” फ़राइज़े-किफ़ाया की सूची बहुत लम्बी है। अल्लामा नववी ने जो बड़े प्रसिद्ध फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन में से हैं, इमाम ग़ज़ाली, अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) और बहुत-से दूसरे लोगों ने लिखा है कि जो उलूम फ़र्ज़े-किफ़ाया हैं उनमें दीनी उलूम तो हैं ही इल्मे-फ़िक़्ह, फ़तवा, उलूमे-क़ुरआन, उलूमे-हदीस, इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह, इनके अलावा जो उलूम फ़र्ज़े-किफ़ाया हैं उनमें चिकित्सा, गणित, और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के इन मैदानों का ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इन निपुणताओं का ज्ञान जिनकी मुस्लिम समाज को ज़रूरत है और जो मुस्लिम समाज की आत्म निर्भरता के लिए अनिवार्य हैं। ये सब उलूम फ़र्ज़े-किफ़ाया हैं।
इसी तरह से इस्लामी अक़ीदों की बौद्धिक व्याख्या और बौद्धिक स्पष्टीकरण की वह दक्षता या वह व्यक्ति जो इस्लाम पर आपत्तियों का जवाब देने के लिए किसी दौर में अनिवार्य हो, वह भी फ़र्ज़े-किफ़ाया है। इसी तरह से तफ़सीर (क़ुरआन की व्याखाया), हदीस और फ़िक़्ह में फ़तवा, क़ज़ा (न्यायशास्त्र) और इज्तिहाद के दर्जों तक पहुँचने के लिए जो दर्जा दरकार है वह विद्वानों के ज़िम्मे फ़र्ज़े-किफ़ाया है। इसलिए कि इज्तिहाद हर दौर की ज़रूरत है। हर दौर में नई समस्याएँ पैदा होती रहेंगी, हर दौर में नई मुश्किलें सामने आती जाएँगी। अगर शरीअत हर दौर के लिए है, जैसा कि वह है, तो हर दौर में इन समस्याओं के जवाब देनेवाले विद्वान भी मौजूद होने चाहिएँ और वे ऐसे विद्वान होने चाहिएँ जो इज्तिहाद के गुणों से विभूषित हों। इज्तिहाद से काम ले सकें। यही वजह है कि इस्लामी विद्वानों ने हर दौर में इज्तिहाद के तक़ाज़ों और इज्तिहाद की ज़रूरी शर्तों पर चर्चा की है।
इज्तिहाद की ज़रूरी शर्तें हर ज़माने के हिसाब से, हर दौर के हिसाब से विभिन्न हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आज के दौर में कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध अर्थशास्त्र और बैंकिंग से है। अर्शशास्त्र और बैंकिंग में आज मुस्लिम समाज को नई-नई समस्याएँ पेश आ रही हैं। इन समस्याओं की समझ के लिए बैंकिंग को समझना ज़रूरी है। इन समस्याओं की वास्तविक बारीकियों का अन्दाज़ा लगाने के लिए, इन समस्याओं के आयामों का अन्दाज़ा लगाने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान ज़रूरी है। अगर किसी आलिम को अर्थशास्त्र और बैंकिंग के आवश्यक नियमों का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए इन समस्याओं में इज्तिहाद करना बहुत मुश्किल होगा। जिस ज़माने में ये समस्याएँ इतनी पेचीदा नहीं थीं, उस ज़माने में भी इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी जैसे व्यक्तित्व ने इस बात की ज़रूरत समझी कि वे बाज़ार में जाकर क्रय-विक्रय के तौर-तरीक़ों को देखें और यह पता चलाएँ कि बाज़ार में क्रय-विक्रय के कौन-कौन से तरीक़े प्रचलित हैं, ताकि वे उनके आदेश संकलित कर सकें। तो अगर इस सादा माहौल में जहाँ क्रय-विक्रय के मामले इतने पेचीदा नहीं हुए थे, जब ये चीज़ें अलग कला के रूप में संकलित नहीं हुई थीं, इमाम मुहम्मद जैसे बुद्धिमान इंसान को इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि वे स्थायी रूप से इन मामलों को जाकर देखें और समझें, तो आज के दौर में ऐसा करना निस्सन्देह अनिवार्य है। अभी मैंने बताया कि मुस्लिम उम्मत या मुस्लिम समाज का आधार ज्ञान पर है। यह ज्ञान वह है जिसमें अक़्ल और नक़्ल (बौद्धिक तथा क़ुरआन और हदीस से प्राप्त ज्ञान) दोनों आ जाते हैं, जो इल्मे-दीन और इल्मे-दुनिया दोनों के मेल-मिलाप पर आधारित है।
ज्ञान की इस्लामी धारणा के अनुसार अक़्ल और नक़्ल में कोई टकराव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) ने इस विषय पर एक बहुत विस्तृत किताब लिखी थी। इसमें अल्लामा ने बहुत सूक्ष्म और व्यापक ढंग से लिखा है कि صریح المعقول لا ینافی صحیح المنقول “स्पष्ट रूप से अक़्ल (बुद्धिसंगत) की बात नक़्ल (क़ुरआन और सुन्नत) के ख़िलाफ़ नहीं होती।” इस व्यापकता का एक बहुत बड़ा सुबूत इस्लामी उसूले-फ़िक़्ह है। उसूले-फ़िक़्ह को जिस ढंग से अइम्मा-ए-उसूल ने संकलित किया। उदाहरणार्थ इमाम ग़ज़ाली ने, उदाहरणार्थ इमाम शातबी ने, उदाहरणार्थ इमाम राज़ी ने, ये वे लोग हैं जो अपने दौर के पहली पंक्ति के तर्कशास्त्र के विद्वानों में शुमार होते हैं। इन्होंने जिस ढंग से उसूले-फ़िक़्ह को संकलित किया उसमें इस दौर के हिसाब से बौद्धिक माँगें पूरे तौर पर समो दी गई हैं। उस ज़माने में बौद्धिकता का सबसे बड़ा उच्चतम स्तर यह था कि लोग यूनानी दर्शन और तर्कशास्त्र में माहिर हों। उस ज़माने में यूनानी दर्शन और तर्कशास्त्र के मानकों के अनुसार इमामुल-हरमैन, इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी आदि ने उसूले-फ़िक़्ह को संकलित कर दिया और इतनी मज़बूत बुनियादों पर संकलित कर दिया कि कोई बड़े-से-बड़ा तर्कशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि उसूले-फ़िक़्ह की अमुक बात बुद्धि के ख़िलाफ़ है। इमाम राज़ी और अल्लामा सैफ़ुद्दीन आमदी जैसे तर्कशास्त्रियों ने तरह-तरह के फ़र्ज़ी सवालात और फ़र्ज़ी सन्देह उठाकर, उनका जवाब देकर यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उसूले-फ़िक़्ह के मामले बुद्धि की अत्यन्त मज़बूत बुनियादों पर क़ायम हैं। इसके साथ-साथ उसूले-फ़िक़्ह के मौलिक लक्ष्य क़ुरआन और सुन्नत से लिए गए हैं, उसूले-फ़िक़्ह के मसाइल (विस्तृत आदेशों) में कोई मसला ऐसा नहीं है जो क़ुरआन और सुन्नत के आदेश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिया न गया हो। इसलिए वहाँ नक़्ल के तक़ाज़े भी पूरे तौर पर मौजूद हैं।
जब तक अक़्ल और नक़्ल का यह सन्तुलन मुसलमानों में मौजूद रहा, जब तक मुस्लिम समाज में वैचारिक स्वतंत्रता, आत्म निर्भरता और क़ुरआन और सुन्नत से सीधा सम्बन्ध मौजूद रहा, उस समय तक मुसलमानों का वैचारिक स्थान नेतृत्व और मार्गदर्शन का रहा। जब यह वैचारिक स्वतंत्रता कमज़ोर पड़ी, जब मुसलमान ग़ैरों की नक़्ल का शिकार हुए तो पहले अरस्तू और अफ़लातून का अनुकरण शुरू हुआ, फिर अरस्तू और अफ़लातून के दर्जे से निचले दर्जे के लोगों का अनुकरण शुरू हुआ और होते-होते जब तक़लीद-पसन्दी (अनुकरणवाद) मुसलमानों के स्वभाव का हिस्सा बन गई तो हर ऐरे-ग़ैरे की तक़लीद शुरू हो गई। आज कैफ़ियत यह है कि हर वह व्यक्ति जो किसी पश्चिमी भाषा में कोई बात लिख दे, या जिसका सम्बन्ध किसी पश्चिमी देश से हो उसकी बात को बिना जाँचे-परखे स्वीकार कर लिया जाता है और अनुकरण के लिए यह कहना काफ़ी है कि अमुक पश्चिमी व्यक्ति ने यह बात यों लिखी है। इसका नतीजा यह निकला कि एक तरफ़ हमारा आधुनिक शिक्षित वर्ग पश्चिम के घटिया-से-घटिया इंसानों के अनुकरण को गर्व की बात समझता है, और जो दीनी वर्ग है वह बादवालों के भी बादवाले उलमा की तक़लीद (अनुकरण) को काफ़ी समझता है और उसकी नज़र में बादवालों के बादवालों ने भी जो लिख दिया है वह शरीअत के मामले में मानो फ़ाइनल है, नतीजा आपके सामने है।
इस्लामी शरीअत में, इस्लामी सभ्यता में प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों के चरित्र को महत्त्व के साथ बयान किया गया है। अगर शरीअत का आधार ज्ञान है तो फिर विद्वानों का चरित्र मौलिक चरित्र होना चाहिए। इस्लामी विद्वानों का चरित्र इस्लामी समाज में अत्यन्त महत्त्व रखता है, जब तक उलमा का चरित्र उच्चस्तरीय और दरकार मानकों के अनुसार होगा, उस समय तक मुस्लिम समाज सही इस्लामी बुनियाद पर क़ायम रहेगा, और जब उलमा का चरित्र और रवैया बदल जाएगा, स्तर से गिर जाएगा, तो मुस्लिम समाज भी उसी हिसाब से स्तर से हटना शुरू हो जाएगा। यही कैफ़ियत अन्य सामूहिक और राजनैतिक नेताओं की है, यानी उलमा अगर दीनी और वैचारिक पेशवा हों तो शेष लोग जो किसी-न-किसी दृष्टि से नेतृत्व के पद पर आसीन हों, वे शासक हों या शासक न हों, वे भी नेतृतव के पद पर आसीन हैं, और इन दोनों की ज़िम्मेदारी है कि मुस्लिम समाज को सही रास्ते पर क़ायम रखें। उलमा और नेताओं की इस महत्त्वपूर्ण भूमिका की ओर इशारा करते हुए अपने समय के बहुत बड़े मुहद्दिस और अमीरुल-मोमिनीन फ़िल-हदीस इमाम अब्दुल्लाह-बिन-मुबारक (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक जगह लिखा है— “दीन के मामलात में बिगाड़ किसने पैदा किया? शासकों ने, और बुरे पेशवाओं और उलमाए-सू (असत्यवादी इस्लामी विद्वानों) ने।” अगर उलमाए-सू मुस्लिम समुदाय में नेतृत्व के पद पर आसीन हो जाएँ, वे उलमाए-सू जो दीन के नाम पर दुनिया कमाना चाहते हों, जो दीन का नाम लेकर अपनी भौतिक माँगों, मन की इच्छाओं और प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहते हों तो मुस्लिम समुदाय के पतन में देर नहीं लगती।
ज्ञान और शिक्षा के बाद मुस्लिम समाज का दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण आधार और विशेष गुण न्याय और इंसाफ़ है। न्याय और इंसाफ़ अपने पूर्ण और वास्तविक अर्थ में न केवल इस्लामी शरीअत का मौलिक लक्ष्य है, बल्कि पवित्र क़ुरआन के अनुसार तमाम आसमानी शरीअतों, आसमानी किताबों, पैग़म्बरों और अल्लाह की तरफ़ से भेजे गए रसूलों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोग न्याय और इंसाफ़ पर क़ायम हो जाएँ। पवित्र क़ुरआन में ‘अद्ल’ और ‘क़िस्त’ की दो शब्दावलियाँ प्रयोग हुई हैं। ये दोनों इंसाफ़ की दो विभिन्न सतहों को बयान करती हैं। ‘अद्ल’ एक ऐसा गुण है जो एक बहुत विस्तृत और व्यापक अर्थ रखता है। इंसान को आदेश दिया गया कि वह अपने-आपसे ‘अद्ल’ करे, अपने ख़ानदान से ‘अद्ल’ करे, समाज से ‘अद्ल’ करे। फिर राज्य को आदेश दिया गया कि वह ‘अद्ल’ से काम ले, समाज में सामूहिक ‘अद्ल’ क़ायम करे, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘अद्ल’ के लिए कोशिश करे। इंसानों के दरमियान आम तौर पर जो लेन-देन का रवैया हो वह ‘अद्ल’ का हो। अल्लाह के दूसरे तमाम स्रष्ट प्राणियों के साथ ‘अद्ल’ और इंसाफ़ का रवैया अपनाया जाए। यह ‘अद्ल’ के वे विभिन्न दर्जे और मरहले हैं जिसका इस्लामी शरीअत ने आदेश दिया है। जो व्यक्ति अपने-आपसे ‘अद्ल’ नहीं कर सकता वह अपने परिवार से ‘अद्ल’ नहीं कर सकता, जो अपने ख़ानदान में ‘अद्ल’ से काम नहीं ले सकता वह समाज में ‘अद्ल’ क़ायम नहीं कर सकता, इसलिए ‘अद्ल’ का आरम्भ सबसे पहले अपने वुजूद से होता है, अपने-आपसे ‘अद्ल’ का अर्थ यह है कि इंसान अपने अन्दर तमाम प्रवृत्तियों और शक्तियों के दरमियान सन्तुलन से काम ले, भलाई और ख़ैर की शक्तियों को विकास दे, ताक़तवर बनाए और बदी की शक्तियों को दबाकर रखे, उनको भलाई की शक्तियों के अधीन कर ले, बुराई की शक्तियों से बुराई का काम लेने के बजाय भलाई का काम ले।
परिवार के दरमियान ‘अद्ल’ से मुराद यह है कि इंसान परिवार के हर व्यक्ति के अधिकार को पूरे तौर पर अदा करे, हर व्यक्ति परिवार के बारे में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरे तौर पर अंजाम दे। समान दर्जा रखनेवाले रिश्तेदारों के दरमियान पूरे ‘अद्ल’ और बराबरी से काम ले, एक से अधिक बेटे हों तो उनके दरमियान न्याय और इंसाफ़ हो, एक से अधिक भाई हों तो उनके दरमियान न्याय और इंसाफ़ हो, एक से अधिक पत्नियाँ हों तो उनके दरमियान न्याय और इंसाफ़ हो। फिर ‘अद्ल’ और इंसाफ़ के तक़ाज़े ये भी हैं कि रिश्तेदारों में जिसका अधिकार शरीअत ने ज़्यादा क़रार दिया है, जो ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार है उसपर उस निकटता के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। यह बात ‘अद्ल’ के ख़िलाफ़ है कि सगे भाई से तो दुश्मनी हो और दूसरे किसी रिश्ते के भाई का लिहाज़ किया जा रहा हो, यह बात न्याय और इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है कि एक बेटा तो बहुत प्यारा हो और दूसरा बेटा प्रकोप का भागी ठहरे। परिवार के दरमियान ‘अद्ल’ क़ायम करना पवित्र क़ुरआन के मौलिक आदेशों और मौलिक माँगों की हैसियत रखता है। एक प्रसिद्ध हदीस में इस बात को क़ियामत की निशानियों में से बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने दोस्तों से तो सद्व्यवहार करे और बाप के साथ दुर्व्यवहार करे, माँ की अवज्ञा करे और बीवी के अकारण नाज़-नख़रे उठाए। ऐसे तमाम रवैये इसलिए ना-पसन्दीदा हैं कि यह ‘अद्ल’ की इस्लामी धारणाओं से टकराते हैं।
पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह जहाँ अपने-आपके बारे में न्याय और सन्तुलन का आदेश दिया गया है, वहाँ परिवार के बारे में भी न्याय एवं सन्तुलन का आदेश दिया गया है। एक आम निर्देश है कि “मुझे आदेश दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान ‘अद्ल’ करूँ।” यह तमाम इंसानों के दरमियान ‘अद्ल’ की बात है। समाज में ‘अद्ल’ क़ायम होगा, लोग एक-दूसरे से न्याय और इंसाफ़ से काम ले रहे होंगे तो फिर राज्य स्तर पर ‘अद्ल’ का प्रबन्ध आसान होगा। आम तौर पर समझा जाता है कि न्याय और इंसाफ़ से मुराद केवल वह न्याय और इंसाफ़ है जो अदालतों के द्वारा, जजों और क़ाज़ियों के द्वारा क़ायम होता है। यह दुरुस्त है कि जजों और अदालतों के द्वारा क़ायम होनेवाला अदल, ‘अद्ल’ का एक बहुत महत्त्वपूर्ण दर्जा है। लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह ‘अद्ल’ के बहुत-से दर्जों में से एक दर्जा है, ‘अद्ल’ के बहुत-से मैदानों में से एक मैदान है। अगर ‘अद्ल’ के शेष मैदान नज़रअन्दाज़ किए जा रहे हों तो मात्र सरकारी या अदालती इंसाफ़ से एक न्यायप्रिय समाज और एक न्यायिक व्यवस्था क़ायम नहीं हो सकती।
इसी लिए शरीअत ने ‘अद्ल’ के सन्दर्भ में जहाँ क़ानूनी इंसाफ़ का आदेश राज्य और राज्य के इदारों को दिया है, वहाँ वास्तविक न्याय का आदेश लोगों को दिया है। हर व्यक्ति को मालूम होता है कि उसके पास जो-जो चीज़ें हैं वे वास्तव में उसकी मिल्कियत हैं या नाजायज़ तौर पर उसके क़ब्ज़े में आई हैं। हर व्यक्ति अपने ख़यालात को बेहतर अन्दाज़ में जानता है, हर व्यक्ति ख़ूब जानता है कि वह जो रोज़ी कमाता है उसमें कितना हिस्सा हलाल है और कितना हराम का है, हर व्यक्ति ख़ूब जानता है कि उसने जिस क़द्र मज़दूरी वुसूल की है, जिस नौकरी की तनख़ाह वुसूल की है, उसमें उसने कितनी ईमानादरी से काम लिया है। उसमें उसने कितना ध्यान लगाया है। यह बात कि तनख़ाह तो महीने के आख़िर में पूरी ले ली जाए और काम आधा भी न हो, यक़ीनन ज़ुल्म है, ‘अद्ल’ के ख़िलाफ़ है और यह आमदनी जायज़ नहीं है। कितने लोग हैं जो इस मामले में ‘अद्ल’ से काम ले रहे हैं।
शरीअत ने राज्य और अदालतों को हस्तक्षेप करने की वहाँ अनुमति दी है जहाँ खुले तौर पर ना-इंसाफ़ी की जा रही हो, जहाँ बिलकुल ज़ाहिरी अन्दाज़ में लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, जहाँ सुबूत और गवाहियों के द्वारा अदालत में साबित किया जा सकता हो, लेकिन जो मामलात अदालतों में आ सकते हैं उनके मुक़ाबले में कई सौ गुना मामलात ऐसे पेश आते हैं जो अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते, लेकिन सम्बन्धित लोगों को मालूम होता है कि उन्होंने किसका अधिकार छीना है, किसके साथ ज़ुल्म किया है, किसके साथ ना-इंसाफ़ी की है, यह उनकी निजी ज़िम्मेदारी, दूसरे शब्दों में फ़र्ज़े-ऐन है कि वे वास्तविक इंसाफ़ से काम लें। जहाँ अदालत के दरवाज़े बन्द हो जाते हैं, जहाँ क़ाज़ी और जज की सतह से बात आगे चली जाती है वहाँ व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। पवित्र क़ुरआन ने इसी को ‘क़िस्त’ के शब्द से याद किया है।
पवित्र क़ुरआन ने केवल ‘क़िस्त’ पर बस नहीं किया, अगर एक व्यक्ति ने ख़ामोशी से किसी की चीज़ चुरा ली और किसी को पता नहीं चला, अदालत को भी पता नहीं चला, पुलिस को पता नहीं चला, कोई गवाह नहीं, कोई सुबूत नहीं, अब यह व्यक्ति ख़ुद तो जानता है कि उसने क्या चीज़ चुराई है, उसकी दीनी, शरई, नैतिक ज़िम्मेदारी है, इसके बारे में क़ियामत के दिन सवाल होगा, कि वह चुराई हुई चीज़ अस्ल मालिक को वापस कर दे और जितनी देर उसको प्रयोग में रखा है उसके लिए अल्लाह से तौबा भी करे और अस्ल मालिक से माफ़ी भी माँगे, लेकिन यह तो मात्र जायज़-नाजायज़ की बात है, शरीअत इंसानों को इससे भी ऊपर ले जाना चाहती है, शरीअत चाहती है कि इंसान अपने नैतिक स्तर में इससे बहुत ऊपर जाएँ। इसलिए शरीअत ने एहसान की नसीहत की है, एहसान वहाँ होता है कि जहाँ किसी व्यक्ति का अधिकार तो नहीं है, क़ानूनी या शरई हक़ तो नहीं बनता, लेकिन आप अधिकार न बनने के बावजूद उसकी ज़रूरत का एहसास करते हुए उसकी ज़रूरत को पूरा करें, आपपर कोई ज़िम्मेदारी क़ानून या शरीअत या नैतिकता ने नहीं डाली, लेकिन आप यह महसूस करते हैं कि अमुक व्यक्ति जिससे आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आपपर उसका कोई बोझ या भार नहीं है, लेकिन आप उसके मामलात को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए उसकी मुश्किल दूर कर देते हैं, यह एहसान है। शरीअत यह आशा करती है कि मुस्लिम समाज में अधिकांश संख्या एहसान करनेवालों की हो, लेकिन यह भी काफ़ी नहीं है, शरीअत में एक दर्जा इससे भी ऊँचा है, और वह दर्जा ‘ईसार’ का है, इसके बारे में ख़ुद पवित्र क़ुरआन का कहना यह है कि अल्लाह के ख़ास ख़ास बन्दे वे हैं। और पवित्र क़ुरआन में उनकी तारीफ़ की गई है, उनमें सबसे पहले प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) शामिल हैं, जो अपनी मुश्किल के बावजूद अपनी ज़रूरत और हाजत के बावजूद, अपने हितों को क़ुर्बान करके अपनी ज़रूरत को नज़रअन्दाज़ करके दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं और ख़ुद तकलीफ़ उठाते हैं, ख़ुद परेशानियों का सामना करते हैं लेकिन दूसरों को परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं, यह रवैया ‘ईसार’ का है। शरीअत ने इन दोनों रवैयों को इस दृष्टि से अनिवार्य या फ़र्ज़ क़रार नहीं दिया कि उनके बारे में दुनिया या आख़िरत में सवाल किया जाएगा, लेकिन अगर कोई यह रवैया अपनाएगा तो आख़िरत में उसके दर्जे असीमित होंगे और दुनिया में उसके प्रभाव से एक ऐसा भला और साफ़-सुथरा समाज बनेगा, जो इस्लाम का उद्देश्य और इस्लाम का लक्ष्य है।
इस्लामी समाज या मुस्लिम उम्मत के बारे में एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए और वह है ‘दूसरों के साथ सम्बन्ध’ के बारे में इस्लाम का नज़रिया, कि ग़ैरों से, ग़ैर-मुस्लिमों से मुसलमान का सम्बन्ध कैसा होता है और मुस्लिम समाज में आबाद वे लोग जो मुस्लिम समाज से सम्बन्ध नहीं रखते उनकी क्या हैसियत है। हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज शुरू से एक मिश्रित यानी plural समाज रहा है, यह बात तो हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, आज भी हर व्यक्ति यह बात जानता है कि मुस्लिम समाज में भाषागत विविधता भी है, विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले मुस्लिम समाज का आज भी इसी तरह हिस्सा हैं जैसे पहले थे। सांस्कृतिक विविधता रखनेवाले आज भी इसी तरह घुल-मिलकर रहते हैं, फ़िक़ही विविधता भी बहुत है, विभिन्न फ़िक़ही मसलकों का अस्तित्व इस बात का सुबूत है कि pluralism मुस्लिम समाज की नस-नस में बसा हुआ है, जहाँ विशुद्ध धार्मिक मामलों में, विशुद्ध फ़िक़ही और दीनी मामलों में विविधता की अनुमति दी जाती है, वहाँ शेष मामलों में विविधता का क्यों स्वागत नहीं किया जाएगा। फिर यह विविधता न केवल फ़िक़ही मामलों और इज्तिहादात में है, बल्कि कलाम और अक़ीदों के बारे में भी है, मुसलमानों में विभिन्न तार्किक प्रवृत्तियाँ देर तक मौजूद रही हैं, एक ही शिक्षक के शिष्यों में एक से अधिक प्रवृत्तियाँ तार्किक समस्याओं के बारे में मौजूद थीं। ख़ुद अहले-सुन्नत में जो मुसलमानों के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी संख्या मुसलमानों में नव्वे प्रतिशत के क़रीब है, उनमें अशअरी, सलफ़ी, हंबली और मातुरीदी, ये सब प्रवृत्तियाँ एक साथ पाई जाती हैं, फिर नस्ली विविधता और नस्ली अधिकता, ऐसी चीज़ है जिससे इस्लामी दुनिया का हर निवासी परिचित है।
इससे भी बढ़कर मुस्लिम समाज में pluralism का एक बड़ा उदाहरण यह है, मिश्रित समाज होने का एक बड़ा प्रमाण यह है, कि मुस्लिम समाज में शुरू से ग़ैर-मुस्लिम निवासियों को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उनको वे तमाम अधिकार और रिआयतें दी गईं जो ख़ुद मुसलमानों को प्राप्त थीं, हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु उन्हु) का यह वाक्य प्रसिद्ध है, फ़िक़ही लिटरेचर में बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है कि “जो ग़ैर-मुस्लिम मुस्लिम जगत् की नागरिकता अपनाते हैं उनके वही अधिकार हैं जो हमारे हैं, उनकी वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमारी हैं।” यह बात विभिन्न इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने विभिन्न ढंग में बयान की है। प्रसिद्ध हनफ़ी फ़क़ीह और फ़िक़्ह हनफ़ी के पहले पंक्ति के अइम्मा और मुज्तहिदीन में से एक हज़रत इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰) ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में बयान किया है कि “मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिम दुनियवी मामलात में एक-दूसरे के बराबर हैं।” यानी उनमें अगर कोई फ़र्क़ रखा जाएगा रवैये में और मामलात में तो क़ियामत के दिन रखा जाएगा। अल्लाह तआला जिसको जो सज़ा देना चाहेगा वह देगा, लेकिन इस दुनिया के मामलात में, आपस में लेन-देन में, आपस में जायदाद के तबादले में, एक-दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा में, एक-दूसरे की जान माल और इज़्ज़त की सुरक्षा में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम सब बराबर हैं।
आज पश्चिमी दुनिया के पेशवाओं और चिन्तकों का दावा है कि उन्होंने उन तमाम भेदभावों को ख़त्म कर दिया है जो इंसानों के दरमियान पाए जाते हैं, यह ज़रा इन मुसलमानों से पूछें जो पश्चिमी दुनिया में रहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कितने भेदभाव समाप्त हो गए हैं। आज कितने मुसलमान हैं जिनको अपने दीन (इस्लाम) के अनुसार पारिवारिक मामले हल करने की अनुमति नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं जो अपनी जायदाद को शरीअत के अनुसार अपने वारिसों में विभाजित नहीं कर सकते। आज कितने मुसलमान हैं जो अपनी प्रतिदिन की इबादतों को सुविधापूर्वक अदा नहीं कर सकते। आज कितनी मुसलमान युवतियाँ और महिलाएँ हैं जिनको इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार वस्त्र तक पहनने की अनुमति नहीं। आज भी यूरोप के, बल्कि यूरोप से प्रभावित बहुत-से देशों में सिखों को दाढ़ी रखने की अनुमति है, मुसलमानों को नहीं। सिखों को पगड़ी बाँधने की अनुमति है, मुसलमानों को टोपी ओढ़ने की अनुमति नहीं।
इसकी तुलना में इस्लामी समाज में ग़ैर-मुस्लिमों को न केवल पूरी आज़ादी और समता प्राप्त रही, बल्कि कुछ ऐसे अधिकार भी प्राप्त रहे जो मुसलमानों को प्राप्त नहीं हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने एक जगह लिखा है कि कुछ पहलुओं से ग़ैर-मुस्लिमों का दर्जा और स्टेटस मुस्लिम समाज में मुसलमानों से बेहतर है। बहुत-से मामलों में उनको वे सुविधाएँ प्राप्त हैं जो मुसलमानों को प्राप्त नहीं हैं। इस्लामी राज्य में ग़ैर-मुस्लिमों को इसकी अनुमति भी दी गई कि वे अपने व्यक्तिगत मामले, अपने धार्मिक मामले, अपने धर्म के अनुसार अंजाम दें और उन्हीं की अदालतें, उन्हीं के क़ाज़ी उनके मामलों का फ़ैसला करें। न केवल नबवी दौर में और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में यहूदियों और ईसाइयों के अपने धार्मिक पेशवा उनके मतभेदों का फ़ैसला करते थे, अपने धार्मिक मामलों को ख़ुद चलाते थे, बल्कि बाद के ज़मानों में भी, बनी-उमय्या के ज़माने में, बनी-अब्बास के ज़माने में, सल्तनते-उस्मानिया के ज़माने में, भारत में सल्तनते-मुग़्लिया के दौर में, उससे पहले दौरे-सल्तनत में, इन तमाम ज़मानों में ग़ैर-मुस्लिमों के मामलात, ग़ैर-मुस्लिम अदालतें, उनकी अपनी व्यवस्था के अनुसार चलाया करती थीं। मिश्रित समाज होने का ऐसा कोई उदाहरण आज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है।
पश्चिमी दुनिया ने अपने तमाम-तर दावों के बावजूद अभी तक मुसलमानों को इसकी अनुमति नहीं दी कि वे अपने व्यक्तिगत क़ानून के अनुसार अपने मामलों का फ़ैसला कर सकें। आज वहाँ भाई-चारा, आज़ादी और समता के नारे तो बहुत लगाए जाते हैं। विशेष रूप से फ़्रांस क्रान्ति के बाद ये नारे बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन इस भाई-चारे का, जिसकी पश्चिमी धारणा दावेदार है, अस्ल अर्थ क्या है? क्या वाक़ई तमाम इंसानों को पश्चिमी दुनिया ने भाई-भाई मान लिया है? क्या पश्चिमी दुनिया अरस्तू और अफ़लातून के ज़माने से प्रचलित इस तसव्वुर से निकल आई है कि पश्चिमी दुनिया शासन करने के लिए है और शेष दुनिया ग़ुलामी करने के लिए है? क्या पश्चिमी दुनिया रोमी मानसिकता से निकल आई है जो अपने को सभ्य और शेष सारे संसार को असभ्य क़रार दिया करते थे? पश्चिमी दुनिया की आज की व्यवस्था देखी जाए, ख़ुद संयुक्त राष्ट्र में इंसानों के विभाजन की प्रक्रिया को देख लिया जाए, पश्चिमी दुनिया के रवैयों को देख लिया जाए, ग्लोबलाइज़ेशन (globalization) के नाम पर क्या हो रहा है, या ISO के नाम पर क्या-क्या बातें हो रही हैं, यह सब इस बात की दलील है कि भाई-चारे से मुराद पश्चिमी दुनिया की आपस का भाई-चारा है, आज़ादी से मुराद पश्चिमी दुनिया की आज़ादी है, समता से मुराद पश्चिमी दुनिया की आपस की समता है, ख़ुद पश्चिमी दुनिया में भी अगर कोई मुसलमान है तो वह ग़ैर-मुस्लिम पश्चिमवालों के बराबर नहीं है। तुर्कों के साथ क्या हो रहा है, अल्बानिया के साथ क्या हो रहा है, बोस्निया के साथ किया हुआ, शेष जो मुस्लिम आबादियाँ हैं, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप में उनके साथ क्या रवैया है। यह सारे रवैये इस बात का प्रमाण हैं कि ये नारे मुस्लिम जगत् में मात्र भाषणों को लुभावना बनाने के लिए और किताबों के शीर्षकों को सजाने के लिए हैं। उनका वास्तविक अर्थ पश्चिमी दुनिया के लिए कम-से-कम मुसलमानों की हद तक कोई अधिक महत्त्व नहीं रखता।
पवित्र क़ुरआन में यह बात तो बार-बार बताई गई कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आख़िरी पैग़म्बर हैं, स्पष्ट रूप से भी है, सांकेतिक ढंग से भी कही गई है और विभिन्न शैलियों से यह बात मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आख़िरी नबी हैं तो उनकी ‘उम्मत’ भी आख़िरी मुस्लिम उम्मत होगी। यह बात चूँकि कम महसूस की जाती है, इसलिए कुछ हदीसों में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। सुनने-इब्ने-माजा की रिवायत है एक जगह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “जिस तरह मैं आख़िरी नबी हूँ उसी तरह तुम आख़िरी ‘उम्मत’ हो।” एक और जगह फ़रमाया गया, “मैं पैग़म्बरों में से तुम्हारे हिस्से में आया हूँ और तुम उम्मतों में से मेरे हिस्से में आए हो।” निश्चय ही यह एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, निश्चय ही यह बहुत बड़ा सम्मान है, निस्सन्देह यह बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य मात्र दर्जे को या सौभाग्य को बयान करना नहीं है, बल्कि यहाँ फ़राइज़ (कर्त्तव्यों) और ज़िम्मेदारियों को बयान करना अभीष्ट है, जो फ़राइज़ रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़िम्मे किए गए थे, उनके इस दुनिया से जाने के बाद वे फ़राइज़ ‘उम्मत’ के ज़िम्मे किए गए हैं। यही वजह है कि पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह ‘उम्मत’ का फ़र्ज़ भलाई का आदेश देना और बुराइयों से रोकना क़रार दिया गया है। अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, यह मुस्लिम समाज के कर्त्तव्यों में सबसे महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है।
ग़ौर किया जाए तो मुस्लिम समाज के सारे फ़राइज़ इन्हीं दो शीर्षकों के तहत आ सकते हैं, यह कर्त्तव्य लोगों का भी है, हर मुसलमान व्यक्ति अपनी सतह पर, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी सीमाओं के अन्दर और अपनी पहुँच के अनुसार अच्छाई का आदेश देने और बुराई को रोकने का पाबन्द है। पवित्र क़ुरआन में एक जगह लुक़्मान हकीम की नसीहत नक़्ल की गई है, यह नसीहत उन्होंने अपने बेटे को की थी, ज़ाहिर है जब बाप बेटे को कोई चीज़ याद दिलाएगा तो उसके निजी कर्त्तव्य, या अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाएगा, इसलिए यहाँ एक ही व्यक्ति को सम्बोधित करते हुए कहा गया, “ऐ बेटा! नमाज़ क़ायम कर।” नमाज़ क़ायम करना हर व्यक्ति की निजी ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़े-ऐन है, कोई और मेरी तरफ़ से या मैं किसी और की तरफ़ से नमाज़ अदा नहीं कर सकता। “और अच्छाई का आदेश दे और बुराई से रोक।” यह व्यक्ति की ज़िम्मेदारी का दर्जा है। दूसरी ज़िम्मेदारी गिरोहों और जमाअतों की है, मुस्लिम समाज में विभिन्न गिरोह भी होंगे जमाअतें भी होंगी, संगठन भी होंगे, क़बीले भी होंगे, बिरादरियाँ भी होंगी, अब सबकी जहाँ अन्य ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ यह ज़िम्मेदारी भी है कि वे अपने क्षेत्र में, अपनी क्षमता के अनुसार अच्छाई का आदेश दें और बुराई से रोकें, उसके बाद राज्य की ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों के बारे में इरशाद है कि “अगर हम उनको ज़मीन में सत्ता सौंप दें तो वे ये चार काम करेंगे।” चार फ़राइज़ बताए गए हैं, “नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, उसका प्रबन्ध करते हैं, अच्छाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं।” ज़ाहिर है जो सतह हुकूमत की होगी वह लोगों की नहीं होगी, जो लोगों की होगी वह गिरोहों और जमाअतों की नहीं होगी। हुकूमत के पास क़ानून की ताक़त है, शासन की ताक़त है, हुकूमत उस सतह पर भलाई का आदेश देगी जहाँ लोगों की सतह समाप्त हो जाती है, जमाअतों और गिरोहों की सतह समाप्त हो जाती है, हुकूमत क़ानून के बल से भी काम लेगी, हुकूमत राज्य की शक्ति भी प्रयोग करेगी और जहाँ लोगों का उपदेश देना नाकाम हो जाता है, जहाँ गिरोहों और जमाअतों का दबाव और बुराई का रोकना नाकाम हो जाता है, वहाँ राज्य की ज़िम्मेदारी शुरू होती है।
राज्य की ज़िम्मेदारी के बाद एक सतह पूरी ‘उम्मत’ की है। “तुम एक उत्तम समुदाय हो जिसे लोगों की भलाई के लिए निकाला गया है।” (क़ुरआन, 3:110) इसमें सभी मुसलमानों को सम्बोधित किया गया है, पूरी ‘उम्मत’ से कहा गया है, मुस्लिम समुदाय की ज़िम्मेदारी है कि वह विश्व स्तर पर, पूरी मानवता के स्तर पर अच्छाई का आदेश दे और बुराई से रोके, यह काम दो सतहों पर होगा, यह ज़िम्मेदारी पूरे मुस्लिम समुदाय की है, इसको दो स्तरों पर पूरा किया जाएगा। एक स्तर तो कथन का है, दूसरा स्तर व्यवहार और रवैये का है। व्यवहार और रवैया मुस्लिम समाज का ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखकर अच्छाई सीखें और बुराई से बचें, लोगों को मालूम हो जाए कि अच्छाई पर अमल इस तरह होता है और बुराई से इस तरह बचा जाता है। क़ौल (कथन) का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति का, या ‘उम्मत’ के अधिकाँश लोगों का प्रशिक्षण ऐसा हो कि उनकी ज़बान से सत्य और भली बात ही निकले, बुरी बात न निकले, वे जहाँ बैठें, जहाँ उठें, अपने कथन और व्यवहार से अच्छाई का उपदेश देनेवाले हों और बुराई से रोकने वाले हों।
ये सभी सामूहिक कर्त्तव्य जो मुस्लिम समाज के हैं, उनको ‘अम्र बिल-मारुफ़’ (भलाई का आदेश देना) और ‘नही अनिल-मुनकर’ (बुराई से रोकना) के अलावा कुछ और शब्दावलियों से भी बयान किया गया है। एक जगह ‘तवासी बिल-हक़’ और ‘तवासी बिस-सब्र’ की शब्दावली प्रयोग हुई है, कि वे एक-दूसरे को हक़ की नसीहत करते हैं और एक-दूसरे को सब्र की भी नसीहत करते हैं। अरबी ज़बान में वसीयत का अर्थ वह नहीं है जो उर्दू में प्रचलित हो गया है, अगरचे वह अर्थ भी वसीयत के अर्थ में शामिल है, वसीयत का अर्थ एक ऐसा निष्ठापूर्ण उपदेश है जो अत्यन्त निष्ठाभाव से की जाए और जिसका उद्देश्य केवल उस व्यक्ति का लाभ या भलाई हो जिसको उपदेश दिया जा रहा है। पवित्र क़ुरआन में आया है, “अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी सन्तान के बारे में वसीयत करता है।” (क़ुरआन, 4:11) ज़ाहिर है यह वसीयत इस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में उर्दू और हिन्दी में यह शब्दावली प्रचलित हो गई है। यहाँ नसीहत और निष्ठापूर्ण उपदेश के अर्थ में यह शब्द प्रयोग हुआ है। ‘तवासी बिल-हक़’ का अर्थ यह है कि ‘उम्मत’ का हर व्यक्ति दूसरे को इतने निष्ठाभाव और दर्दमन्दी से नसीहत करे कि इस दर्दमन्दी का असर सुननेवाला महसूस करे। कभी-कभी हक़ की नसीहत की ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी सब्र की नसीहत की ज़रूरत पड़ती है। अगर विमुखता किसी नेमत के नतीजे में पैदा हो तो हक़ की नसीहत करनी चाहिए और अगर विमुखता किसी आज़माइश या मुश्किल के नतीजे में पैदा हो तो सब्र की नसीहत करनी चाहिए।
यह बात कि मुस्लिम समुदाय में कोई बुराई पैदा हो रही हो और आम सतह पर इसका नोटिस न लिया जाए, यह बात इस्लामी सोच के ख़िलाफ़ है। इस्लामी शिक्षा यह है कि ‘एहतिसाब’ (Accountability) और ग़लत को ग़लत कहना मुस्लिम समाज की मौलिक ज़िम्मेदारी है। ‘एहतिसाब’ का अर्थ यह है कि जहाँ जो बुराई हो रही हो उसको इसी सतह पर रोकने की कोशिश की जाए, व्यक्ति की सतह पर हो रही हो तो व्यक्ति उसको रोके, परिवार में हो रही हो तो परिवार के बुज़ुर्ग और ज़िम्मेदार लोग उसको रोकें, औलाद को मना करें, समझाएँ, शिक्षा दें, समाज में हो रही हो तो समाज में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, पहले नसीहत के साथ, ख़ामोशी के साथ, फिर सन्तुलित व्यवहार के साथ, फिर शिक्षा-प्रशिक्षण के द्वारा, फिर शेष सामाजिक उपायों के द्वारा।
पवित्र क़ुरआन में इस बात को सख़्त नापसन्द ठहराया गया है कि समाज में बुराई हो रही हो और लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठा रहे हों। पवित्र क़ुरआन में एक जगह किसी पिछली क़ौम का उल्लेख किया गया और यह बताया गया कि अल्लाह तआला ने उस क़ौम के तमाम लोगों को तबाह कर दिया, जो इस बुराई में मुब्तला थे उनको भी, और जो बुराई में मुब्तला नहीं थे उनको भी तबाह कर दिया, इसलिए कि “जो बुराई में मुबतला नहीं थे वे दूसरों को उस बुराई से रोकते नहीं थे।” (क़ुरआन, 5:79) उनकी ज़िम्मेदारी थी कि रोकने की कोशिश करते, और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए वे भी मुजरिम क़रार पाए और सामूहिक अज़ाब का वे भी शिकार हुए।
विभिन्न हदीसों में कुछ सामूहिक परिणामों का ज़िक्र किया गया है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से बतौर सज़ा के लागू किए जाते हैं। जिस क़ौम में अमुक बुराई पैदा होगी उसको उस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिस क़ौम में अमुक बुराई पैदा होगी उसको अमुक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। बज़ाहिर ये परिणाम सबके सामने आते हैं और लोग महसूस भी करते हैं कि यह अमुक गुनाह की सज़ा है, इस तरह की सज़ाएँ भी जब समाज में आती हैं तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, इसलिए कि कुछ लोग तो उस बुराई को करते हैं और कुछ लोग जो बुराई ख़ुद तो नहीं करते लेकिन दूसरों को नहीं रोकते, इसलिए वे भी इसका शिकार होते हैं।
यही वजह है कि ‘उम्मत’ के कर्त्तव्यों में यह बात बताई गई कि यह बुराई को रोकने का काम करती है, समाज की जाँच करती है और एक-दूसरे को हक़ और सब्र की नसीहत करती है। यह सब्र और हक़ की नसीहत यह एहतिसाब और यह बुराई से रोकना हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों में कोई संगठित चर्च नहीं है, दीनदारों का कोई वर्ग अलग से नहीं है। यहाँ दीन की रस्में बिना किसी चर्च के अदा होती हैं, यहाँ कोई वर्ग दीनदार या रूहानियों का नहीं है, हर व्यक्ति का सम्बन्ध दीनदार वर्ग से है, और हर व्यक्ति का सम्बन्ध जनसाधारण के वर्ग से है। जिन धर्मों में दीनदारों का वर्ग अलग से क़ायम किया गया उनकी आईडियल सोच क्या थी, और वास्तविकता और व्यवहार क्या है, इसके अधिक विवरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतिहास का अवलोकन यह है कि वह आईडियल और वह कल्पना एक दिन के लिए भी व्यवहार में नहीं आ सकी। इसके विपरीत इस्लाम का अनुभव कि बिना किसी संगठित चर्च के धार्मिक रस्मों को अदा किया जाए, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह से सम्बन्ध क़ायम करे, यह अनुभव व्यवहारतः आज भी उतना ही सफल है जितना पहले दिन था।
धार्मिक जीवन का संगठन मुस्लिम समाज स्वचलित ढंग से करता आया है, आज भी जहाँ कोई मुस्लिम आबादी कुछ घरों की भी मौजूद हो, वहाँ मस्जिद क़ायम हो जाती है, वहाँ क़ुरआन की शिक्षा के लिए दर्सगाह शुरू हो जाती है, वहाँ धीरे-धीरे मस्जिद की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वक़्फ़ भी क़ायम हो जाते हैं, कुछ जगह प्रशिक्षण और दीनी शिक्षा की संस्थाएँ भी क़ायम हो जाती हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि मुस्लिम समाज में एक स्वचलित कार्यप्रणाली ऐसी मौजूद है जो बिना संगठित चर्च के, बिना संगठित धार्मिक वर्ग के, दीनी मामलों और दीनी रस्मों को ख़ुद-ब-ख़ुद अंजाम देता चली जाती है।
मुस्लिम समाज में कुछ विशिष्टताएँ रही हैं, ये विशिष्टताएँ आज भी मौजूद हैं, इस्लामी समाज एक सतह पर आज भी इस्लामी शरीअत पर कार्यरत समाज है, सम्भव है कि यह बात कुछ लोगों को अजीब-सी लगे, हम तो यह बात करते और सुनते आए हैं कि मुस्लिम समाज इस्लामी शरीअत पर कार्यरत नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज इस्लामी शरीअत पर कार्यरत है, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। निश्चय ही मुसलमानों में बहुत-सी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, निश्चय ही मुस्लिम समाज में शरीअत की बहुत-सी शिक्षाओं पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन इन सब कमज़ोरियों के बावजूद मुस्लिम समाज एक हद तक शरीअत के आदेशों पर अमल कर रहा है।
आप बच्चे के जन्म से लेकर और उसके निकाह और दाम्पत्य जीवन और मरने तक के मामलों को देखें, तमाम महत्त्वपूर्ण दर्जों और महत्त्वपूर्ण सरगर्मियों का जायज़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे मुसलमानों की है जो अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों में आज भी शरीअत के आदेशों और मुसलमानों की परम्पराओं का पालन करते हैं। यहाँ तक कि उन मुस्लिम इलाक़ों में भी, जहाँ लम्बे समय तक कम्युनिज़्म का, या दूसरी नास्तिकतावादी शक्तियों का वर्चस्व रहा, जहाँ धर्म से जुड़ाव को अपराध क़रार दे दिया गया था, जहाँ धार्मिक शिक्षा देना अपराध था जिसकी सज़ा मौत थी, वहाँ भी अधिकांश मुसलमान अपने प्रतिदिन के जीवन में, पारिवारिक मामलों में, मरने और जीने के मामलों में, जन्म और निकाह और शादी ब्याह और तलाक़ के मामलात में शरीअत के आदेशों का ख़ामोशी से पालन करते रहे।
आज से कुछ समय पहले मुझे भूतपूर्व सोवियत यूनियन में जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ, वहाँ कुछ ज़िम्मेदार लोगों से मुलाक़ात हुई, एक बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति ने यह बयान किया कि पिछले सत्तर वर्ष में कम्युनिज़्म के ज़माने में, ऐसा कोई उदाहरण नुमायाँ तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया, यह उसने बयान किया कि जहाँ किसी मुसलमान मरनेवाले ने यह वसीयत की हो कि उसकी आख़िरी रस्में कम्युनिस्ट तरीक़े के अनुसार अंजाम दी जाएँ, हर व्यक्ति की वसीयत यह होती थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े-बड़े लीडर भी शामिल होते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के उच्चतम अधिकारी भी शामिल होते थे, लेकिन मरते समय उनकी वसीयत यह होती थी कि उनको इस्लामी तरीक़े के अनुसार दफ़न किया जाए। यह मात्र छोटा-सा उदाहरण इस बात का है कि शरीअत पर कार्यरत रहना, शरीअत की व्यवस्था से जुड़े रहना, मुस्लिम समाज से अपने सम्बन्ध या मुस्लिम समाज की सदस्यता को बरक़रार रखना, यह मुसलमानों की नस-नस में आज भी मौजूद है।
मुस्लिम समाज की विशिष्टता की एक और निशानी बुद्धि और वह्य (ईश-प्रकाशना) का संगम भी है। यों तो बुद्धि और वह्य का संगम पूरी इस्लामी शरीअत, इस्लामी ज्ञान-विज्ञान और मुसलमानों की पूरी ऐतिहासिक परिपाटी की विशिष्टता रही है, लेकिन जीवन के जिस पहलू में यह विशिष्टता सबसे नुमायाँ होती है, वह फ़िक़्ह और उसूले-फ़िक़्ह के मैदान हैं। इन दोनों मैदानों में एक साथ अक़्ल और नक़्ल, यानी बुद्धि और वह्य दोनों के तक़ाज़े समान रूप से पूरे किए जाते हैं।
मुस्लिम समाज की विरली विशेषताओं में भलाइयों में आगे बढ़ने को भी शामिल किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे समाजों में भलाइयों में आगे बढ़ने की भावना मौजूद नहीं है, इसका अर्थ यह है कि यह बात मुस्लिम समाज में जितनी नुमायाँ है, उतनी नुमायाँ दूसरे समाजों में नहीं है। यह बात कि कोई व्यक्ति अपने नाम से कोई संस्था क़ायम कर दे और वर्षों तक उसका नाम प्रसिद्ध हो जाए, वर्षों उसकी सन्तान उसके नाम से फ़ायदा उठाए, ये बातें तो बहुत हैं, सांसारिक ख्याति की ख़ातिर, भौतिकवाद की ख़ातिर, टैक्स से बचने की ख़ातिर इस तरह की संस्थाएँ बना दी जाएँ, यह बात तो विभिन्न क़ौमों में मौजूद है, लेकिन यह बात कि केवल अल्लाह की प्रसन्नता की ख़ातिर बिना किसी नामो-नुमूद के, बिना किसी विज्ञापन और सांसारिक उद्देश्य के इंसान अपनी ज़िन्दगी की कमाई क़ुर्बान करे, यह बात केवल मुस्लिम समाज में पाई जाती है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं — हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में मौजूद हैं — जो केवल अल्लाह की प्रसन्नता की ख़ातिर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, और भलाइयों में आगे बढ़ने के वे नमूने क़ायम करते हैं जिनकी मिसाल ग़ैर-इस्लामी दुनिया में मुश्किल से मिलेगी।
ख़ुद मस्जिदों की मिसाल ले लें, मुसलमानों की कौन-सी बस्ती आज ऐसी है जहाँ मस्जिदें अधिक संख्या में मौजूद न हों। आज कोई मुस्लिम आबादी ऐसी है जहाँ मुसलमानों ने नमाज़ों का आयोजन न किया हो, जहाँ दस घर भी मुसलमानों के मौजूद हैं, वहाँ कोई-न-कोई मस्जिद अस्तित्व में आ जाती है, वहाँ पवित्र क़ुरआन की शिक्षा-प्रशिक्षण का कोई-न-कोई प्रबन्ध हो जाता है। इसी वजह से नमाज़ों का आयोजन, जुमा और ईदैन (ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़हा) की नमाज़ों का प्रबन्ध, और अज़ान का प्रबन्ध जो मुसलमानों की निशानियों में एक निशानी है, हर बस्ती में मौजूद है। ग़ैर-मुस्लिम देशों में मुस्लिम बस्तियाँ हों, बड़े-बड़े ग़ैर-मुस्लिम शहरों में छोटी-छोटी मुस्लिम आबादियाँ हों, नमाज़ों का आयोजन हर जगह मौजूद है। ज़कात और सदक़ात का प्रबन्ध हर जगह मौजूद है। हज का आयोजन हर जगह मौजूद है। रमज़ानुल-मुबारक में जो आध्यात्मिक वातावरण महसूस होता है, बड़े मुस्लिम देशों में, प्राचीन इस्लामी शहरों में वह आध्यात्मिक वातावरण हर मस्जिद में और हर इस्लामी केन्द्र में महसूस होता है। पश्चिमी देशों के बड़ी-बड़ी राजधानियों में और शहरों में, जहाँ-जहाँ मस्जिदें या इस्लामी केन्द्र मौजूद हैं, रमज़ान के दिनों में, रमज़ान की रातों में, इफ़्तार और सहरी के समय और तरावीह के समय वहाँ का वातावरण बिलकुल अलग होता है। यह समानता जो हाँगकाँग से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तटों तक, और स्वीडन से लेकर कैपटाउन तक हर जगह नज़र आती है, यह मुस्लिम समाज की विशिष्टता का एक नमूना है। इस तरह की विशिष्टता दूसरे धर्मों में मुश्किल से मिलेगी।
अभी ज़िक्र किया गया कि मुस्लिम समाज के दो मौलिक आधार हैं, एक ज्ञान, दूसरा अद्ल यानी न्याय। ज्ञान से जुड़ाव अगरचे बहुत कमज़ोर हो गया है, अगरचे ज्ञान की धारणा मुसलमानों ने सीमित कर दी है, अगरचे ज्ञान से सम्बन्ध की वह कैफ़ियत अब क़ायम नहीं रही जो अभीष्ट है। लेकिन इन सबके बावजूद दीन (धर्म) के ज्ञान से सम्बन्ध मुस्लिम समाज में आज भी मौजूद है। कोई मुस्लिम बस्ती ऐसी नज़र नहीं आएगी यहाँ तक कि कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में भी नहीं थी, जहाँ खुले या ख़ुफ़िया तौर पर दीनी शिक्षा की संस्थाएँ मौजूद न हों, जिन दिनों सोवियत यूनियन में धार्मिक शिक्षा देना अपराध था, जिसकी सज़ा मौत थी, उन दिनों भी वहाँ अंडरग्राउंड दीनी शिक्षा की दर्सगाहें मौजूद थीं, उन दिनों भी वहाँ ख़ुफ़िया तौर पर पवित्र क़ुरआन और दीनी शिक्षा की संस्थाएँ काम कर रही थीं, मैंने ख़ुद ऐसी संस्थाएँ देखी हैं जो अंडरग्राउंड क़ायम थीं, जो इस तरह बनाई गई थीं कि उनमें होनेवाली बातचीत की आवाज़ बाहर न जाए। वहाँ पढ़ानेवाले कुछ बुज़ुर्गों को मैंने देखा है। एक बुज़ुर्ग को मैंने देखा है जो फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाया करते थे, उन्होंने 1920 ई॰ के लगभग शिक्षा पूरी की थी और 1920 ई॰ से लेकर 1990 ई॰ तक वे यह शिक्षा देते रहे। सत्तर साल उन्होंने शिक्षा दी, जब मैं उनसे मिला तो उनकी उम्र सौ साल के क़रीब थी। उन्होंने बताया कि उनके पास फ़िक़्हे-हनफ़ी की प्राचीन किताबों के जो नुस्ख़े थे, वे सत्तर साल के लम्बे समय तक प्रयोग के बाद अब इस योग्य नहीं रहे कि उनको और अधिक प्रयोग किया जा सके। अगर यह भावना और यह क़ुर्बानी मुस्लिम समाज की विशिष्टता नहीं है, तो फिर विशिष्टता और किसे कहते हैं।
जहाँ तक ‘अद्ल’ का सम्बन्ध है, इसमें निस्सन्देह मुसलमानों से कोताहियों हुई हैं, मुस्लिम समाज की विशिष्टता जो ‘अद्ल’ में नुमायाँ हुई थी, आज वह विशिष्टता बहुत कमज़ोर पड़ गई है। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज में ‘अद्ल’ की उस धारणा को ज़िन्दा किया जाए और उस विरली विशेषता को दोबारा क़ायम किया जाए, जिससे मुस्लिम समाज दूसरों से अलग नज़र आता था।
मुस्लिम समाज की एक और विरली विशेषता या विशिष्टता वह मज़बूत जनाधार था, जिसने हर दौर में इस्लामी नैतिकता, इस्लामी चरित्र और समाज की इस्लामी संरचना की सुरक्षा की। आज भी मुस्लिम समाजों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनकी उपस्थिति में कोई गुमराही पनप नहीं सकती, वे हर कमज़ोरी को ग़लत कहते हैं और आवाज़ बुलन्द करते हैं। कुछ आधुनिकतावादी लोग इस मामले को मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता क़रार देते हैं।
स्पष्ट रहे कि रूढ़िवाद या आधुनिकतावाद मात्र निरर्थक शब्दावलियाँ हैं। न कोई चीज़ मात्र इसलिए बुरी है कि वह प्राचीन है, न कोई चीज़ केवल इसलिए अच्छी है कि नई है। अच्छाई और बुराई का पैमाना नया या पुराना होना नहीं है, यह धारणा पश्चिम के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने पैदा की है, इसलिए कि वे बड़े व्यापक स्तर पर कारख़ानों से चीज़ें तैयार करते हैं और हर नई चीज़ को लोकप्रिय क़रार देना और पुरानी चीज़ को अप्रिय क़रार देना उनके हितों का हिस्सा है। अगर हर पुरानी चीज़ बुरी और हर नई चीज़ अच्छी न हो तो नए उत्पादन कैसे बिकेंगे, नए-नए मार्केटें कैसे अस्तित्व में आएँगे? इसलिए इस मामले में चलती हुई बातों और प्रचलित शब्दावलियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र चिन्तन, बौद्धिकता और ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए।
किसी भी क़ौम की मौलिक धारणाएँ, मौलिक सिद्धान्त और तथ्य, इतिहास की निरन्तरता की ज़मानत देनेवाली घटनाएँ, ये हमेशा प्राचीन होती हैं, कोई क़ौम, विशेष रूप से कोई ज़िन्दा क़ौम, अपनी प्राचीन परम्पराओं को आसानी से नहीं छोड़ती। पश्चिमी जगत् में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि कुछ मामूली और हास्यास्पद परम्पराएँ तक ऐसी हैं जिनपर पश्चिमी दुनिया आज तक अमल कर रही है और बड़े गर्व से उन परम्पराओं को ज़िन्दा किए हुए है।
इसके मुक़ाबले में पूर्वी दुनिया को यह सबक़ पढ़ा दिया गया है कि तुम्हारी हर प्राचीन चीज़ बुरी है, और हर नई चीज़ जो पश्चिम के व्यापारी, राजनेता, लेखक या संवाददाता प्रचलित करना चाहें वह अच्छी है और स्वीकार्य है। जब तक मुस्लिम समाज इस सिद्धान्त पर कार्यरत रहेगा कि इस्लामी नैतिकता, इस्लामी धारणाएँ और मुस्लिम समाज की बुनियादें मुसलमानों के लिए सबसे बहुमूल्य पूँजी की हैसियत रखती हैं और सुरक्षा के योग्य हैं, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और क़ीमती हैसियत रखती हैं, और उसके ख़िलाफ़ उठनेवाली हर कोशिश, हर आवाज़ और हर कार्रवाई के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए और आवाज़ बुलन्द करनी चाहिए, उस समय तक मुस्लिम समाज की यह विशिष्टता क़ायम रहेगी।
हम कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज शरीअत का समाज है, मुस्लिम समाज एक आध्यात्मिक समाज है। जिनमें आध्यात्मिक मूल्य आज भी कार्यरत हैं, आज भी ऐसे लोग मुस्लिम समाज में मौजूद हैं जो विशुद्ध आध्यात्मिक बुनियादों पर, और अल्लाह के साथ सम्बन्ध की भावना से बहुत-से काम करते हैं। जिनकी ज़िन्दगी का मात्र प्रेरक अल्लाह की प्रसन्नता होता है। मुस्लिम समाज आज भी नैतिक समाज है, नैतिक धारणाएँ अगर इंसानों के किसी समाज में आज भी मौजूद हैं तो वह मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज आज़ादी का समाज होना चाहिए, यह एक आज़ाद समाज है, ग़ुलामी को स्वीकार नहीं करता। यह अजीब अन्तर्विरोध है कि पश्चिमी दुनिया एक तरफ़ आज़ादी के नारे बुलन्द करती है, मुसलमान नौजवान उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन पश्चिम की ग़ुलामी भी उसी अनुपात से बढ़ती जा रही है।
मुस्लिम समाज ‘अद्ल’ और भाई-चारे का समाज है, मुस्लिम समाज का मौलिक गुण जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है न्याय और इंसाफ़ होना चाहिए, भाई-चारे और बिरादरी की भावनाएँ होनी चाहिएँ। इसलिए कि बिरादरी और भाई-चारे की भावनाओं के बिना ‘अद्ल’ क़ायम नहीं किया जा सकता। ‘अद्ल’ के बिना समता क़ायम नहीं हो सकती, जबकि मुस्लिम समाज का मौलिक गुण समता है जो हर दौर में अलग और नुमायाँ रही है। लेकिन अफ़सोस यह है कि उपमहाद्वीप में मुसलमानों ने हिंदुओं की वर्ण-व्यवस्था का असर क़ुबूल किया और यहाँ समता का वह नमूना पेश न कर सके जो इस्लाम की विशिष्टता रही है। अगर मुसलमान उपमहाद्वीप में इस्लामी समता का पूर्ण नमूना पेश करते और यहाँ के पिछड़े वर्गों को वह सम्मान देते जो इस्लाम ने दिया है, उनको मानवता के इस उच्चतम स्थान पर आसीन समझते जिसपर पवित्र क़ुरआन ने इंसानों को आसीन किया है तो भारत के पिछड़े वर्गों में शायद कोई एक भी ऐसा न बचता जो इस्लाम के दामन में पनाह न लेता, लेकिन चूँकि उपमहाद्वीप में इस्लाम ऐसे इलाक़ों से आया था जहाँ बादशाही व्यवस्था की परम्पराएँ बहुत पुरानी थीं, जहाँ अरबों की सादगी और समता की धारणाएँ कमज़ोर या हल्की थीं, इसलिए उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से उत्तरी भारत के इलाक़ों में इस्लामी समता के वी निशानियाँ देखने में नहीं आ सकीं जो समाज की विशिष्टता हैं।
आज ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम जगत् में आम तौर से और पश्चिम जगत् में विशेष रूप से इस्लाम की समता की धारणा को ज़िन्दा किया जाए और वह समाज ताज़ा किया जाए जिसका आधार समता पर, परस्पर सहयोग पर, सन्तुलन पर और मानता के सम्मान पर क़ायम हो।
मुस्लिम समाज हर दौर में एक सत्यवादी समाज रहा है, सत्यवादिता की निशानियाँ आज भी मुस्लिम जगत् में जगह-जगह देखने में आती हैं। विशेष रूप से दीनी मामलों में, नैतिक मामलों में, मुस्लिम समाज किसी भटकाव को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता है। इस विशेषता को पश्चिमी दुनिया में कभी-कभी नकारात्मक रूप से देखा गया और इस ख़ूबी को ख़राबी क़रार दिया गया। वहाँ चूँकि सत्य और न्याय और नैतिक माँगें, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक सिद्धान्त, एक व्यक्तिगत राय की हैसियत रखते हैं, इसलिए वहाँ कोई व्यक्ति किसी नैतिक भटकाव पर आवाज़ बुलन्द नहीं करता, इसलिए कि किसी की व्यक्तिगत राय के बारे में दूसरे को आपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए।
जब मुस्लिम समाज किसी विमुखता और पथभ्रष्टता के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करता है, किसी नैतिक ख़राबी के ख़िलाफ़ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो पश्चिमी जगत् को अजीब-सा महसूस होता है। वे लोग यह अन्दाज़ा नहीं कर पाते कि यह मात्र किसी राय से मतभेद नहीं है, इसलिए कि ये मामलात राय के मामलात नहीं हैं। ये सत्य और न्याय के मामलात हैं, ये नैतिकता और अनैतिकता के मामलात हैं, पवित्र क़ुरआन ने इसपर जगह-जगह ज़ोर दिया है। पवित्र क़ुरआन ने एक जगह और स्पष्ट रूप से बताया है कि एक क़ौम पर अज़ाब आया, उस क़ौम में कुछ नैतिक बुराइयाँ मौजूद थीं, लेकिन जब अज़ाब आया तो सबपर आया इसलिए कि “जो लोग बुर काम नहीं करते थे वे बुरे काम करनेवालों को रोकते नहीं थे।” (क़ुरआन, 5:79) इसलिए मुनकर (बुराई) के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द न करना, उसको ग़लत न कहना, उसकी सार्वजनिक स्तर पर बुराई को बयान न करना, यह मुस्लिम समाज में अप्रिय समझा गया और इस्लामी नैतिकता के ख़िलाफ़ समझा गया। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह बात बार-बार बयान की और ताकीद के साथ इस बात के महत्त्व को बयान किया। एक जगह मुस्नदे-इमाम अहमद में, इमाम हाकिम की मुस्तदरक में और बज़्ज़ार की सुनन में यह रिवायत बयान हुई है कि जब यह मरहला आ जाए कि मुस्लिम समुदाय में ख़ौफ़ और डर पैदा हो जाए, वे किसी ज़ालिम को ज़ालिम कहने से गुरेज़ करें, ख़ौफ़ महसूस करने लगें तो फिर यह इस बात की दलील है कि मुस्लिम समुदाय का ‘उम्मत’ होना ख़त्म हो रहा है और ‘उम्मत’ की धारणा विदा हो रही है। एक और रिवायत है जिसको हदीस के इमामों में से कई बुज़ुर्गों ने बयान किया है, इमाम अबू-दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसई जैसे बुज़ुर्गों ने इसको बयान किया है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि जब मुस्लिम समाज में यह कैफ़ियत पैदा हो जाए कि ज़ालिम ज़ुल्म करे और लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाएँ, उसको ज़ुल्म से न रोकें तो इसका ख़तरा मौजूद है कि अल्लाह तआला का अज़ाब सबको ले डूबे और सब उसका शिकार हों। यह बात इसलिए भी ज़रूरी है कि मुस्लिम समाज एक ‘उम्मते-दावत’ (आवाहक समुदाय) है। इस बात को विस्तार से बयान किया जा चुका है कि ‘अम्र बिल-मारुफ़’ (भलाई का आदेश देना) और ‘नही अनिल-मुनकर’ (बुराई से रोकना) मुस्लिम ‘उम्मत’ के मौलिक कर्त्तव्यों में से है। मुस्लिम समुदाय इसी लिए ‘ख़ैरे-उम्मत’ (कल्याणकारी समुदाय) क़रार दिया गया कि वह अच्छाई का आदेश देता है और बुराई से रोकता है।
एक प्रसिद्ध हदीस में जिसको बहुत-से मुहद्दिसीन और इतिहासकारों ने बयान किया है, हज़रत रबई-बिन-आमिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो प्रसिद्ध सहाबी हैं, उन्होंने रुस्तम के दरबार में स्पष्ट रूप से यह बयान किया है कि अल्लाह तआला ने हमें इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह के बन्दों को इंसानों की बन्दगी से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ़ ले जाएँ, दुनिया की तंगियों से निकालकर विशालताओं में ले जाएँ, दुनिया की व्यवस्थाओं और दूसरे धर्मों के ज़ुल्म से निकालकर इस्लाम के ‘अद्ल’ में लोगों को ले जाएँ। यह मानो एक विश्वव्यापी सन्देश है जो पूरी मानवता के लिए मुस्लिम समाज के ज़िम्मे लगाया गया है।
इस्लाम की ओर आमन्त्रण की और भलाई की एक अनिवार्य माँग यह भी है कि मुस्लिम समुदाय में बुराइयों का और अश्लीलता का प्रसार कम-से-कम हो, अगर कोई कोशिश ऐसी की जाए कि मुस्लिम समुदाय में किसी अप्रिय या अनैतिक हरकत को रिवाज दिया जाने लगे तो पूरे मुस्लिम समुदाय को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में अश्लीलता का प्रचार हो उनको दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और आख़िरत में भी सज़ा मिलेगी। इससे यह इशारा भी मिलता है कि इस्लामी राज्य की यह ज़िम्मेदारी है कि क़ानून के द्वारा उन लोगों के लिए सज़ा निर्धारित करे जो मुस्लिम समाज में अश्लीलता फैलाना चाहते हों। यह अश्लीलता किसी भी नाम से फैलाई जा रही हो, कभी-कभी संस्कृति के नाम से फैलाई जाती है, कभी-कभी आज़ादी के नाम से फैलाई जाती है, कभी-कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से फैलाई जाती है। जिस नाम से भी अश्लीलता फैलाई जा रही हो, यह अपराध होना चाहिए और इस्लामी समाज में इसकी सज़ा होनी चाहिए।
जनसाधारण की यह ज़िम्मेदारी भी है कि जहाँ वे शासकों के अनुपालन के पाबन्द हैं, जहाँ उनको अधिकारियों के आज्ञापालन का आदेश दिया गया है, वहाँ यह भी कहा गया है कि वे ग़लत मामलों में किसी की पैरवी न करें। उनका कर्त्तव्य ही यह है कि “अल्लाह तआला की अवज्ञा जहाँ हो रही हो, वहाँ वह किसी की आज्ञाकारिता नहीं दिखा सकते।” पवित्र क़ुरआन में जहाँ फ़िरऔन की क़ौम की बुराई बयान की गई और उनको फ़ासिक़ (उल्लंघनकारी) यानी दुष्कर्मी क़रार दिया गया, वहाँ उनके अपराधों में यह भी बताया गया है कि “फ़िरऔन ने अपनी क़ौम को बहुत हल्का समझा और क़ौम ने भी उसकी पैरवी की।” (क़ुरआन, 43:54) अत: जहाँ फ़िरऔन मुजरिम था वहाँ उसकी क़ौम भी मुजरिम थी, जिसके आज्ञापालन और पैरवी की वजह से वह यह सब कुछ कर सकी। एक और क़ौम का पवित्र क़ुरआन में ज़िक्र है, “हर दमनकारी की पैरवी करने में वे आगे-आगे रहते थे, हर दुश्मन की पैरवी करने को तैयार रहते थे।” (क़ुरआन, 11:59) इसलिए “उनपर इस दुनिया में भी लानत की गई और आख़िरत में तो लानत की ही जाएगी।” (क़ुरआन, 11:60)
ये वे कुछ विशिष्टताएँ हैं जो मुस्लिम समाज के बारे में पवित्र क़ुरआन और हदीसों में बयान हुई हैं। मुस्लिम समाज की स्थापना जैसा कि बताई गई थी, इस्लाम का सबसे बड़ा सामूहिक लक्ष्य है। इसी मुस्लिम समाज की सुरक्षा के लिए राज्य की ज़रूरत है, इस मुस्लिम समाज के रास्ते में पैदा होनेवाली या पैदा की जानेवाली रुकावटें दूर करने के लिए जिहाद का आदेश दिया गया, इसी मुस्लिम समाज के शिक्षा-प्रशिक्षण के लिए वे सारे निर्देश दिए गए जो शरीअत और फ़िक़्ह की किताबों में दर्ज हैं।
Recent posts
-

इस्लामी शरीअत का भविष्य और मुस्लिम समाज का सभ्यता मूलक लक्ष्य (शरीअत : लेक्चर# 12)
02 December 2025 -

इस्लामी शरीअत आधुनिक काल में (शरीअत : लेक्चर# 11)
25 November 2025 -

इल्मे-कलाम अक़ीदे और ईमानियात की ज्ञानपरक व्याख्या एक परिचय (शरीअत : लेक्चर# 10)
21 November 2025 -

अक़ीदा और ईमानियात - शरई व्यवस्था का पहला आधार (शरीअत : लेक्चर# 9)
17 November 2025 -

तज़किया और एहसान (शरीअत : लेक्चर# 8)
12 November 2025 -

तदबीरे-मुदन - राज्य और शासन के सम्बन्ध में शरीअत के निर्देश (शरीअत : लेक्चर# 7)
05 November 2025

