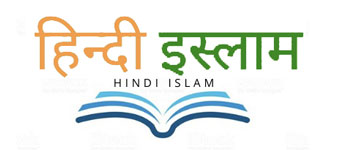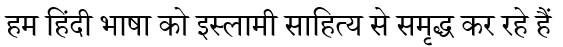तदबीरे-मुदन - राज्य और शासन के सम्बन्ध में शरीअत के निर्देश (शरीअत : लेक्चर# 7)
-
शरीअत
- at 05 November 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
‘तदबीरे-मुदन’ का शाब्दिक अर्थ तो शहरों के प्रबन्ध या राज्यों के प्रबन्ध के हैं, लेकिन परिभाषा की दृष्टि से ‘तदबीरे-मुदन’ से मुराद वे तमाम मामले हैं जिनको आजकल राजनीतिशास्त्र, हुकूमत और राज्य के प्रशासन से व्याख्यायित करते हैं। इस्लामी चिन्तकों ने ‘तदबीरे-मुदन’ के शीर्षक से जो चर्चाएँ की है वे आजकल संवैधानिकता, राजनीतिशास्त्र और दर्शन तथा नैतिकता की बहुत-सी बहसों पर सम्मिलित हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि इस्लामी चिन्तकों ने तत्त्वदर्शिता की मौलिक रूप से दो बड़ी-बड़ी क़िस्में क़रार दी थीं। एक तत्त्वदर्शिता वैचारिक और दूसरी तत्त्वदर्शिता व्यावहारिक। व्यावहारिक तत्त्वदर्शिता अर्थात् रणनीति से मुराद वह तत्त्वदर्शिता है जिसका उद्देश्य नैतिकता की धारणा, और उच्च चरित्र को व्यवहारतः व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य में क़ायम करना अभीष्ट हो। इस्लाम की बौद्धिक, वैचारिक और सांसकृतिक परम्परा के अनुसार, इस्लाम की शिक्षाओं की रौशनी में मात्र वैचारिक बहसों का कोई ख़ास महत्त्व नहीं है। इस्लाम कोई मात्र वैचारिक एवं काल्पनिक सन्देश नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक सन्देश है जो इंसानों की इस दुनिया में व्यापक और भरपूर परिवर्तन का उद्देश्य सामने रखता है। इस धारणा के सामने इस्लामी चिन्तकों ने जहाँ तत्त्वदर्शिता के वैचारिक पहलू से चर्चा की है, अक़ीदे (आस्था), नैतिकता और आध्यात्मिकता की निरी धारणाओं पर बात की है, वहाँ उन्होंने इस बात को भी बहुत ज़रूरी समझा है कि इन धारणाओं के व्यावहारिक गठन यानी अभीष्ट व्यक्ति की तैयारी, परिवार के प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण तथा फिर राज्य और समाज के प्रबन्ध और प्रशिक्षण पर भी चर्चा की जाए।
तदबीर का शब्द अत्यन्त महत्त्व रखता है। तदबीर एक भरपूर और व्यापक शब्दावली है जो दूसरी दो शब्दावलियों के साथ प्रयुक्त होती है। एक ‘इबदाअ’, दूसरी ‘ख़ल्क़’, तीसरी ‘तदबीर’। ‘इबदाअ’ से मुराद है किसी चीज़ को बिना किसी अस्ल या बिना किसी पदार्थ या पिछली कल्पना के मात्र अनस्तित्व से अस्तित्व में ले आना। यह ‘इबदाअ’ कहलाता है। यह सिर्फ़ अल्लाह तआला का काम है, यह सिर्फ़ अल्लाह तआला की शान है कि वह सृष्टि को अनस्तित्व से अस्तित्व में ला सकता है। ‘इबदाअ’ के बाद ‘ख़ल्क़’ का दर्जा है। ‘ख़ल्क़’ पारिभाषिक अर्थ में उस प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ पिछले पदार्थ से या मौजूद स्थितियों और शक्लों की मदद से कोई नई सूरत और शक्ल पैदा करना अभीष्ट हो। यह काम मौलिक रूप से अल्लाह तआला का है, लेकिन कभी-कभी और कहीं-कहीं वह इंसानों को भी इसका ज़रिया बनाता है। उसने एक सीमित सतह पर यह क्षमता इंसानों को भी दी है कि वे विभिन्न पदार्थों और आकृतियों को सामने रखकर नई-नई आकृतियाँ और नए-नए नमूने संकलित कर सकते हैं। चुनाँचे पवित्र क़ुरआन में हल्का-सा इशारा इस बात का भी मिलता है कि यह रचनात्मक गुण अल्लाह तआला ने इंसानों को भी दिया है। एक जगह कहा गया है “क्या ही बरकतवाला है अल्लाह जो तमाम रचनाकारों से बढ़कर है।” (क़ुरआन, 40:14) यहाँ ‘ख़ालिक़’ (रचयिता) का शब्द बहुवचन के तौर पर प्रयोग हुआ है। जो इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि ‘ख़ल्क़’ (रचना करने) का गुण एक सीमित और निर्धारित अर्थ में अल्लाह तआला ने इंसानों को भी प्रदान किया है।
‘ख़ल्क़’ के बाद तीसरी शब्दावली ‘तदबीर’ की है। तदबीर से मुराद है पैदा हो चुकीं चीज़ों का प्रबन्ध। अल्लाह तआला की तदबीर दो तरह की होती है। एक तदबीर ‘तकवीनी’ कहलाती है, जो सृष्टि के स्वाभाविक क़ानून का नाम है। अल्लाह तआला ने इस सृष्टि के लिए जो क़ानून निर्धारित किए, जिनको ‘क़ानूने-तबीइया’ (भौतिक नियम) का नाम दिया जा सकता है वे ‘तदबीरे-तकवीनी’ के दायरे में आते हैं, उनको तदबीरे-तकवीनी भी कहा जाता है। तदबीरे-तकवीनी के बाद ‘तदबीरे-तशरीई’ है जिसके अनुसार अल्लाह तआला ने पैग़म्बरों के द्वारा निर्देश अवतरित किए, शरीअतें उतारीं, इन शरीअतों का उद्देश्य ही इंसानी मामलों की तदबीर और प्रबन्ध है। यह तदबीर व्यक्ति की भी होती है, परिवार की भी होती है, राज्यों और समाजों की भी होती है। तदबीर के उन्हीं पहलुओं के सामने इस्लाम के बड़े विद्वानों ने ‘तदबीरे-मंज़िल’ और ‘तदबीरे-मुदन’ की दो शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं।
तदबीरों की इन दो क़िस्मों के अलावा एक तदबीर इंसानी भी होती है। इंसान अपने मामलात की तदबीर और प्रबन्ध करता है। अपने मामलात का इन्तिज़ाम और प्रबन्ध करता है। इनसानी तदबीर अगर तदबीरे-तशरीई की हदों में काम करे और तदबीरे-तकवीनी की अपेक्षाओं से अपने को मिला ले तो वह कामयाब रहती है, लेकिन अगर तदबीरे-इंसानी तदबीरे-तशरीई से फिर जाए तो वह तदबीर दरअसल तदबीर नहीं, बल्कि तबाही बन जाती है।
तदबीर की इस परिकल्पना को समझने के लिए ज़रूरी है — विशेष रूप से यहाँ हमारा विषय चूँकि तदबीरे-तशरीई है, इसलिए तदबीरे-तशरीई को समझने के लिए ज़रूरी है — कि हम यह ज़ेहन में रखें कि शरीअत देनेवाले ने, जो शरीअत प्रदान की है उसके दो मौलिक उद्देश्य हैं, या दो मौलिक लक्ष्य हैं। एक मौलिक लक्ष्य तो यह है कि इंसानों तक शरीअत के आदेश, शरीअत की हदें और नियम, कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ सब पहुँच जाएँ। इंसानों को मालूम हो जाए कि उनके लिए तशरीई आदेश क्या हैं? उनके कार्यक्षेत्र की हदें क्या है? उनके ज़िम्मे कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?
शरीअत का दूसरा बड़ा लक्ष्य यह है कि इंसानों को यह मालूम हो जाए कि उनका वास्तविक और निजी हित किस चीज़ में है और वास्तविक और निजी नुक़सान किस चीज़ में है? यानी वास्तविक निहितार्थ क्या है और वास्तविक बिगाड़ क्या है? इंसान बहुत-सी चीज़ों को भला समझता है, लेकिन वास्तव में वे भली नहीं होतीं। इंसान अपनी सीमित बुद्धि एवं ज्ञान से कुछ मामलों को भलाई नहीं समझता। हालाँकि वहाँ भलाई होती है। इसी तरह से कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको शरीअत ने फ़साद (बिगाड़) क़रार दिया है, और उनको मफ़ासिद (बिगाड़ों) के दायरे में रखा है, लेकिन इंसान की सीमित बुद्धि और समझ उनके बिगाड़ होने को समझ नहीं पाती। इसलिए शरीअत ने आदेश बयान करने के साथ-साथ जगह-जगह ऐसा मार्गदर्शन भी उपलब्ध किया है जिसके द्वारा भलाई का भलाई होना और बिगाड़ों का बिगाड़ होना मालूम हो जाए। जब ये बिगाड़ और भलाइयाँ मालूम हो जाएँ तो उनके द्वारा स्वयं को सुधारने का काम बहुत आसान हो जाता है।
इंसान अपने नफ़्स (अन्तर्मन) का सुधार कैसे करे? अपने दिल के आन्तरिक गठन की प्रक्रिया कैसे पूरी करे? तदबीरे-मंज़िल की ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाए? जिसको आदाबे-मईशत (अर्थव्यवस्था के शिष्टाचार) कहा गया है उसके तक़ाज़े कैसे पूरे करे? और फिर आख़िरकार जिसको ‘सियासते-मुदन’ या ‘तदबीरे-मुदन’ कहा जाता है वे ज़िम्मेदारियाँ कैसे अंजाम दी जाएँ। यानी जनसाधारण के आपस के मामलात और लेन-देन को कैसे संगठित और संकलित किया जाए। ये सब मामले उसी समय दुरुस्त तरीक़े से अंजाम पा सकते हैं, जब मौलिक रूप से भलाई और बिगाड़ का ज्ञान हो और यह मालूम हो जाए कि भलाई क्या है और बिगाड़ क्या है?
जिसको सियासते-मुदन कहा जाता है या जिसके लिए इस्लामी विद्वानों ने ‘तदबीरे-मुदन’ की शब्दावली प्रयुक्त की है उसमें मुल्की और प्रशासनिक मामले भी शामिल हैं, इसमें बड़ी हद तक सामाजिक सम्बन्ध और कारक भी शामिल हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और लेन-देन के मामले भी शामिल हैं। गोया इंसानों के पारस्परिक मामलों में जो अनेकता है, वह भी ‘तदबीरे-मुदन’ या राज्य तथा राजनीति के प्रबन्धन में ज़ेरे-बहस आती है। आजकल धार्मिक अनेकता यानी रिलीजियस पुलुरलिज़्म (Religious Pluralism) की बात बहुत अधिक हो रही है। दुनिया का आग्रह है कि सफल समाज वही है जो अपनी एकता में अनेकता को स्वीकार करता हो, और अनेकता में एकता की तलाश करने में सफल रहा हो।
इस्लाम में पहले दिन से, धार्मिक अनेकता पूरी तरह मौजूद है। आन्तरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। इस्लाम में पहले दिन से अनेक फ़िक़ही मसलक मौजूद हैं। अनेक कलामी मज़ाहिब मौजूद हैं, सूफ़ियाना सिलसिलों का अस्तित्व लम्बे समय से है। इन सबके दरमियान शान्तिपूर्ण परस्पर कार्य विधि भी पहले दिन से तय है। ‘अदबुल-इख़्तिलाफ़’ के नाम से जो फ़न (कला) इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने संकलित किया, वह इसी धार्मिक अनेकता या तत्त्वों की बहुलता को संगठित करने के लिए था। इस्लामी इतिहास में विभिन्न मसलकों के माननेवालों के दरमियान कभी-कभी संघर्ष भी रहा है। यह रस्साकशी फ़िक़ही धर्मों में तो ज़्यादा नहीं रही और अगर रही तो बिल्कुल नाम मात्र थी और ज्ञानपरक बहसों और मुनाज़राना नोक-झोंक तक सीमित थी। सूफ़ियाना सिलसिलों में किसी प्रकार का संघर्ष बिलकुल नहीं रहा। जहाँ कहीं यह संघर्ष ज़ाहिर हुआ वह कलामी मज़ाहिब के दरमियान हुआ। कहीं शीया-सुन्नी मतभेदों के रूप में सामने आया कहीं हंबली और अशअरी मतभेदों के रूप में सामने आआ। कहीं ख़ारिजी और सुन्नी मतभेद के रूप में सामने आया। ये सब मौलिक रूप से कलामी दृष्टिकोण थे। अक़ीदों की मौलिक धारणाओं और इस्लामी अक़ीदों (धारणाओं) के ज्ञानपरक गठन में मतभेद के आधार पर यह मदरसे या मसलक अस्तित्व में आए।
‘तदबीरे-मुदन’ के विषय या बहसों पर जब इस्लाम के बड़े विद्वानों ने ग़ौर किया तो उनके ग़ौर करने के विभिन्न ढंग थे। किसी ने इसको विशुद्ध फ़िक़ही विषय की दृष्टि से संकलित किया। जिन लोगों ने फ़िक़ही दृष्टि से ‘तदबीरे-मुदन’ के विषयों को संकलित किया, उनकी दिलचस्पी का महत्त्वपूर्ण और बड़ा मैदान फ़िक़ही क़ानूनों और आदेशों को संकलित करना था। उन्होंने राज्य, राजनीति और समाज से सम्बन्धित फ़िक़ही मामलात में इज्तिहाद से काम लिया और वे आदेश संकलित किए जिनका उद्देश्य यह था कि राज्य और जनसाधारण के दरमियान सम्पर्कों को बनाया जाए, शासकों की ज़िम्मेदारियों का निर्धारण किया जाए, इस्लामी राज्य के मौलिक क़ानूनों को संगठित किया जाए। इस तरह एक ऐसी शैली सामने आई जिसको आप फ़ुक़हा की शैली कह सकते हैं। फ़ुक़हा की शैली के अनुसार जिन लोगों ने ‘तदबीरे-मुदन’ की बहसों पर ग़ौर किया, उन्होंने उसके लिए ‘अहकामे-सुल्तानिया’ की शब्दावली भी प्रयोग की, कुछ दूसरे फ़ुक़हा ने ‘सियासते-शरीआ’ की शब्दावली भी प्रयोग की। इस्लाम के बड़े विद्वानों में जिन लोगों ने इस विषय पर किताबें लिखीं उनमें इमाम अबू-यूसुफ़ (रह॰), इमाम अबुल-हसन मावर्दी, उनके हंबली साथी इमाम अबू-याला शामिल हैं। उनके अलावा बदरुद्दीन इब्ने-जमाआ फिर आगे चलकर अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) भी इस मैदान में बहुत नुमायाँ हैं। इन सब लोगों ने ‘तदबीरे-मुदन’ की बहसों पर फ़िक़ही अन्दाज़ से ग़ौर किया। एक दूसरी शैली, मुतकल्लिमीन की शैली थी। मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने जब इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की बहसों को संकलित किया तो जहाँ वे इस्लाम के अक़ीदों (धारणाओं) को ज्ञानपरक ढंग से बौद्धिक तर्कों के साथ संकलित कर रहे थे वहाँ उन्होंने राज्य और इमामत की समस्याओं को भी इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की बहसों में शामिल करना ज़रूरी समझा। इसके दो कारण थे। एक आन्तरिक कारण तो यह था कि मुसलमानों में शीया लोगों ने इमामत और राज्य को दीन के मौलिक स्तम्भों में से क़रार दिया। उसूले-दीन में से एक महत्त्वपूर्ण अस्ल इमामत को समझा। अहले-सुन्नत (सुन्नियों) ने इसको उसूले-दीन में से क़रार नहीं दिया। इस्लाम के बड़े विद्वान लिखते हैं कि “दीन के मौलिक सिद्धान्तों और बहसों में राज्य की स्थापना की समस्या शामिल नहीं है।” अब यह बात कि क्या राज्य की स्थापना और इमामत की स्थापना उसूले-दीन में से नहीं है? क्या राज्य की स्थापना आम फ़राइज़ और वाजिबात में से है। यह मात्र एक फ़िक़ही मसला नहीं रहा, बल्कि कलामी मसला बन गया।
बाह्य कारण यह था कि जब यूनानी धारणाएँ मुसलमानों में आम हुईं, मुसलमानों के ज्ञानपरक क्षेत्रों में यूनानी धारणाओं पर वाद-विवाद की प्रक्रिया शुरू हुई तो मुसलमान विद्वानों ने देखा कि यूनानियों के यहाँ राज्य की बहसें बहुत महत्त्व रखती हैं। अफ़लातून ने लोकतंत्र में और अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र में इस विषय पर बहुत बहसें की हैं। ये बहसें मुसलमानों में भी ज़ेरे-बहस आईं। इसलिए मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने भी चाहा कि इन मामलात के बारे में इस्लाम के दृष्टिकोण को भी बौद्धिक तर्कों के साथ इस तरह बयान करें कि वह यूनानी ज्ञान-विज्ञान के विशेषज्ञों के लिए समझने योग्य हो जाए। इस तरह राज्य और राजनीति या ‘तदबीरे-मुदन’ का मामला इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) का हिस्सा बन गया। मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने इसपर ग़ौर किया। इस्लाम के दृष्टिकोण को उन्होंने बौद्धिक तर्कों से बयान किया। जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, यानी शीया चिन्तक, उनका खंडन किया। शीया चिन्तकों ने अहले-सुन्नत की धारणाओं का खंडन किया और अपने अक़ीदों और विचारों को तर्कों द्वारा बयान किया। यों समय गुज़रने के साथ-साथ राज्य और राजनीति का मसला इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की महत्त्वपूर्ण समस्याओं में शामिल हो गया।
मुतकल्लिमीन के साथ-साथ दार्शनिकों ने भी इस विषय से बहस की। सम्भवतः मुसलमानों में सबसे पहला चिन्तक और फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक) जिसने ‘तदबीरे-मुदन’ के विषयों से विशुद्ध बौद्धिक और दार्शनिकतापूर्ण अन्दाज़ में बहस की है वह अबू-नस्र फ़ाराबी है। अबू-नस्र फ़ाराबी ने राज्य और इमामत के मामले को विशुद्ध दार्शनिक सन्दर्भ में देखा और दार्शनिकतापूर्ण तर्कों के अनुसार उसको बयान किया। कुछ कम समझ लोग यह कहने में संकोच नहीं करते कि अबू-नस्र फ़ाराबी ने यूनानी विचारों को अरबी में लिखकर मुसलमानों में आम कर दिया। आंशिक रूप से ऐसा कहना शायद दुरुस्त हो, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। यक़ीनन अबू-नस्र फ़ाराबी, इब्ने-सीना, इब्ने-मस्कवैह, तुफ़ैल, इब्ने-बाजा, ये सब लोग मौलिक रूप से यूनानी दर्शन के विशेषज्ञ थे। और यूनानी दर्शन की समस्याओं और बहसों से सम्बन्ध रखना ही उनके ज्ञान का अस्ल मैदान था। लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि इन लोगों ने इस्लामी धारणाओं को बयान करना अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझा। ऐसा कहना बिलकुल ग़लत और वास्तविकता के ख़िलाफ़ है। अबू-नस्र फ़ाराबी से लेकर बाद के तमाम बड़े-बड़े दार्शनिक और चिन्तक तक, मुल्ला सदरुद्दीन शीराज़ी और मुल्ला जलालुद्दीन दवानी तक, बल्कि आगे चलकर ‘शम्स बाज़िग़ा’ के लेखक मुल्ला महमूद जौनपुरी और उलमाए-ख़ैराबाद तक। इन सब लोगों ने राज्य और इमामत के बारे में इस्लामी धारणाओं को भी बयान किया है और उन बौद्धिक और दार्शनिकतापूर्ण तर्कों से काम लिया है जो दार्शनिकों के यहाँ लोकप्रिय थे। जो यूनानी तर्क शैली उनके यहाँ प्रचलित थी, जिस वर्णन शैली से वे परिचित थे उस तर्क शैली और वर्णन शैली के अनुसार उन्होंने इस्लाम की धारणाओं को बयान किया है। राज्य और इमामत के बारे में इस्लामी धारणाओं को दार्शनिक भाषा में दुनिया के सामने पेश किया।
इन लोगों ने ऐसी नई बहसें भी दर्शन में शामिल कीं जो यूनानियों के यहाँ नहीं पाई जाती थीं। उदाहरणार्थ यूनानियों के यहाँ पैग़म्बरी की परिकल्पना नहीं थी। उदाहरणार्थ यूनानियों के यहाँ फ़रिश्तों की कोई परिकल्पना नहीं थी। यूनानियों के यहाँ आख़िरत की धारणाएँ इतनी नुमायाँ नहीं थीं। लेकिन इन इस्लामी चिन्तकों ने, इन दार्शनिकों ने इन तमाम बहसों को अपनी-अपनी व्यवस्था में जगह दी और इस तरह समोया कि एक नई दार्शनिक परम्परा ने जन्म लिया।
मुसलमानों में राजनीति दर्शन का इतिहास बहुत प्राचीन है। अबू-नस्र फ़ाराबी से पहले से शुरू होता है और अन्त तक आता है। दूसरे बाद के विद्वानों में जिन लोगों ने इस्लाम के राज्य की परिकल्पना और इमामत को विशुद्ध बौद्धिक और दार्शनिकतापूर्ण ढंग से बयान किया उनमें उपमहाद्वीप के चिन्तक आज़म शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰), उनके नामवर बेटे शाह अब्दुल-अज़ीज़ (रह॰) और उनके नामवर पोते, दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध मुजाहिद, चिन्तक और विद्वान मौलाना मुहम्मद इस्माईल शहीद (रह॰) के नाम शायद सबसे नुमायाँ हैं।
दार्शनिकों के साथ-साथ इतिहासकारों ने भी ‘तदबीरे-मुदन’ के विषय से बहस की और इतिहास के अध्ययन की रौशनी में जो विचार या धारणाएँ उनके सामने आईं उनसे काम लेकर उन्होंने इस्लाम के आदेशों और नियमों को बयान किया। निज़ामुल-मुल्क तूसी, इब्ने-ख़लदून, हमारे उपमहाद्वीप में ज़्याउद्दीन बरनी, ये लोग वे हैं जिनकी शैली को इतिहासकारों की शैली कहा जा सकता है। इब्ने-ख़लदून ने तो ख़ैर अपनी शैली स्वयं आरम्भ की, वे उसके संकलनकर्ता भी हैं, और उनको एक विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन इब्ने-ख़लदून से पहले भी ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने राज्य और हुकूमत के इस्लामी आदेशों और धारणाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ बयान किया। ऐतिहासिक दृष्टि से उन विषयों को देखा और ऐतिहासिक शैली के अनुसार ही उनको संकलित किया।
इतिहास से मुसलमान विद्वानों को आरम्भ ही से दिलचस्पी रही है। शायद सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के दौर में, पहले व्यक्ति जिन्होंने दुनिया के इतिहास से दिलचस्पी ली, वह हज़रत मुआविया इब्ने-अबी-सुफ़ियान (रह॰) हैं, जो विभिन्न क़ौमों के इतिहास और उनकी घटनाओं का विवरण जानने से बहुत दिलचस्पी रखते थे और अपने समय का एक ख़ास हिस्सा उन्होंने इस काम के लिए विशिष्ट किया था कि ईरान, रोम, भारत और अजम (ग़ैर-अरब) के शासकों के उत्थान-पतन का घटनाओं की जानकारी प्राप्त करें। बाद में भी यह अध्ययन विभिन्न शासकों की दिलचस्पी का विषय रहा है। शासकों की दिलचस्पी को सामने रखते हुए अनेक इतिहासकारों ने क़ौमों के उत्थान-पतन और राज्यों के आरम्भ और पतनों के बारे में अत्यन्त बुद्धिपरक चर्चा की जो इस्लामी राजनैतिक चिन्तन के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।
इतिहासकारों के साथ-साथ एक शैली साहित्यकारों की भी है। अरबी भाषा में ‘अदीब’ का शब्द एक आम अर्थ के लिए प्रयोग होता था, बल्कि यह कहा जाए तो शायद ग़लत नहीं होगा कि आजकल जिस शब्द को सभ्यता या सिविलाइज़ेशन कहा जाता है ‘अदब’ (साहित्य) का शब्द प्राचीन इस्लामी दौर में क़रीब-क़रीब उसी अर्थ में प्रयोग होता था। मुसलमान आलिमों के नज़दीक ‘अदब’ में मात्र अभिव्यक्ति या वर्णन शैली या भाषा शैली शामिल नहीं थी, बल्कि ‘अदब’ में वे तमाम चीज़ें शामिल थीं जिनका सम्बन्ध किसी क़ौम के सांस्कृतिक प्रतीकों से होता है। चुनाँचे ‘अदब’ की जो परिभाषाएँ प्राचीन साहित्यकारों से उद्धृत हैं, उनमें ‘अदब’ की इसी व्यापकता को समोने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने साहित्यिक शैली के अनुसार राज्य और राजनीति की बहसों को बयान किया उनमें इब्ने-अब्दे-रब्बिह, अल्लामा क़लक़शन्दी और ऐसे अनेक लोग शामिल हैं जिन्होंने विशुद्ध साहित्यिक पैराए में इन नियमों और सिद्धान्तों को जमा करने की कोशिश की, जो क़ौमों के उत्थान-पतन में आम तौर से और राज्यों के आरम्भ और पतन में विशेषकर मौलिक भूमिका निभाते रहे हैं।
‘तदबीरे-मुदन’ पर ग़ौर करने के लिए ये पाँच बड़ी-बड़ी शैलियाँ थीं जिनका संक्षिप्तीकरण और सार पेश करना आज की चर्चा का अभीष्ट है। हमारे उपमहाद्वीप के सबसे बड़े इस्लामी चिन्तक हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के लेखों में इन सब शैलियों की झलक मिलती है। शाह साहब बहुत बड़े मुतकल्लिमे-इस्लाम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, क़ुरआन के टीकाकार भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, फ़ल्सफ़ी (दार्शनिक) भी हैं, सूफ़ी भी हैं। इसलिए उनके यहाँ ये सारी शैलियाँ इकट्ठी मिलती हैं, और उन सबकी झलकियाँ उनके लेखों में मौजूद हैं। इससे पहले एक-आध चर्चा में शाह साहब के इर्तिफ़ाक़ात की धारणा का उल्लेख किया जा चुका है। शाह साहब इंसानी समाज के विकास को सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक विकास को ‘इर्तिफ़ाक़’ की शब्दावली से याद करते हैं। जैसे-जैसे इंसानी समाज विकास करता जाता है राज्य भी विकास करता है जिस तरह समाज के विकास के चार चरण शाह साहब ने बयान किए हैं उसी तरह राज्य के विकास के चार दर्जे भी उन्होंने बयान किए हैं।
सबसे आरम्भिक दर्जा आदिवासी समाज का है जो पहली बार राज्य के रूप में संगठित हुआ हो और उसने शहरी राज्य की बुनियाद डाली हो। शहरी राज्य की जब बुनियाद पड़ती है तो सबसे पहला काम वह किया जाता है जिसको शाह साहब ने ‘तदबीराते-नाफ़िआ’ के नाम से याद किया है। यानी वे तमाम उपाय अपनाए जाते हैं जो जनसाधारण के लिए लाभकारी हों, सामूहिक विकास की गारंटी देते हों और जिनके नतीजे में जनसाधारण की ज़िन्दगी बेहतर-से-बेहतर होती चली जाए। ‘इर्तिफ़ाक़ात’ के ये सिद्धान्त वे हैं जिनपर मानवता आरम्भ से सहमत चली आ रही है। कोई क़ौम कोई शहरी राज्य और कोई इंसानी आबादी इन धारणाओं से ख़ाली नहीं होती। गोया ये वे स्वाभाविक इंसानी धारणाएँ हैं जो तमाम इंसानों के नज़दीक मान्य हैं और सब इंसान उन धारणाओं पर अमल करते हैं। यह बात कि एक व्यक्ति अपना लिबास, अपना आवास, अपना भोजन साफ़-सुथरा रखना चाहता है, उसके स्तर को उच्च से उच्चतर करना चाहता है। यह भावना सब इंसानों में समान रूप से पाई जाती है। इस भावना में पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का भी कोई भेद नहीं है। इस मामले में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में भी कोई अन्तर नहीं है। सिवाय इसके कि मुसलमान इस भावना की पूर्ति में शरीअत की सीमाओं का पाबन्द है। नैतिकता के सिद्धान्तों की पैरवी करता है। ग़ैर-मुस्लिम शरीअत की सीमाओं का पाबन्द नहीं है। कुछ ग़ैर-मुस्लिम नैतिक सीमाओं का पालन करते हैं, कुछ नहीं करते।
शाह साहब ने लिखा है कि नैतिकता के निर्धारित सिद्धान्तों एवं नियमों से विमुख केवल दो प्रकार के लोग होते हैं और वे संख्या में बहुत थोड़े होते हैं। लेकिन अगर आरम्भ में उनका हाथ न रोका जाए तो वे समय के साथ-साथ ज़्यादा प्रभावशाली और ताक़तवर होते जाते हैं। एक तो वे असभ्य, निर्बुद्धि और मूर्ख लोग होते हैं जिनकी दिलचस्पियाँ जानवरों की दिलचस्पियों से ऊँची नहीं होतीं। उनको केवल खाने-पीने और शारीरिक माँगों की पूर्ति से दिलचस्पी होती है। उनकी नज़र में पावनता, पाकीज़गी और सुथराई बेमानी है। दूसरा वर्ग उन लोगों का होता है जो खुले उल्लंघनकारी हैं। जिनको नैतिक सत्ता से चिड़ है। जिनको आध्यात्मिक धारणाओं से बैर है। वे इन सीमाओं को अपनी पाशविक इच्छाओं के रास्ते में रुकावट समझते हैं। इन दो सीमित वर्गों के अलावा मानवता की अधिकांश बहुसंख्या नैतिकता एवं सभ्यता के इन नियमों से सहमति व्यक्त करती है और उनका पालन करती है। जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है इंसानी समाज इन धारणाओं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अपने-अपने अनुभवों के आधार पर नए नियम और नए सिद्धान्त निकालते हैं। इस प्रक्रिया को शाह साहब ने ‘राय-कुल्ली’ की शब्दावली से याद किया है।
मानव समाजों में जो लोग अपनी समझ और सूझ-बूझ में नुमायाँ होते हैं, वे इन नियमों और धारणाओं की खोज और संकलन में दूसरों से नुमायाँ होते हैं। ज्ञान एवं चिन्तन का विकास धीरे-धीरे होता रहता है। शाह साहब ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि ‘इर्तिफ़ाक़े-अव्वल’ यानी इंसानी समाज के विकास का सबसे पहला दर्जा जिन निशानियों और बुनियादों पर सम्मिलित है, पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह उनका उल्लेख किया गया है। पवित्र क़ुरआन ने बाद के ‘इर्तिफ़ाक़ात’ की तरफ़ इशारे ज़्यादा नहीं किए। इसकी वजह है कि ये निशानियाँ हर इंसानी समाज में विभिन्न हो सकती हैं। उच्च सांस्कृतिक निशानियाँ किसी इलाक़े में कुछ होंगी और किसी इलाक़े में कुछ और होंगी। किसी क़ौम में एक तरह की होंगी दूसरी क़ौम में किसी और तरह की होंगी। इसलिए पवित्र क़ुरआन ऐसे तथ्यों और सुबूतों को बयान नहीं करता जो आम इंसानों में समान रूप से न पाए जाते हों। चूँकि ‘इर्तिफ़ाक़े-अव्वल’ की निशानियाँ तमाम इंसानों में समान हैं। मिसाल के तौर पर ज़बानें हैं, मिसाल के तौर पर खेती-बाड़ी की व्यवस्था है, मिसाल के तौर पर जानवरों से काम लेना है, मिसाल के तौर पर घर-बार का निर्माण है। ये वे मामलात हैं जो हर इलाक़े और हर ज़माने में होते हैं। सांस्कृतिक विकास की हर सतह पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने इन्हीं का उल्लेख किया है और इन्हीं को बतौर मिसाल और सुबूत बयान किया है। आगे के दर्जों को उनपर ‘क़ियास’ (अनुमान) किया जा सकता है।
‘फ़न्ने-तदबीरे-मंज़िल’ या ‘सियासते-मदीना’ के आधार पर जब राज्य क़ायम हो जाता है और वह विकास का एक चरण तय कर लेता है, यानी सभ्यता एवं उन्नति के दूसरे चरण में शामिल हो जाता है, तो फिर नए-नए ज्ञान-विज्ञान पैदा होते हैं। अर्थव्यवस्था का ज्ञान पैदा होता है। मामलों के विस्तृत नियम पैदा होते हैं। तत्त्वदर्शिताएँ नए-नए ढंग से सामने आती हैं। यह वह दौर होता है जब उस क्षेत्र के निवासी या उस राज्य के नागरिक अपने रवैये से यह तय करते हैं कि उनका रास्ता विकास और स्थायित्व का रास्ता है या उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह तबाही और बर्बादी का रास्ता है।
शाह साहब ने राज्यों के उत्थान-पतन के कारणों पर भी चर्चा की है और उत्थान-पतन के सामाजिक और नैतिक कारणों के साथ-साथ आर्थिक कारणों पर चर्चा की है। मिसाल के तौर पर उन्होंने यह कहा है कि अगर राज्यों और हुकूमतों के ख़र्चे, संसाधनों से बढ़ जाएँ, बैतुल-माल पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका नतीजा राज्य के पतन के रूप में निकलता है। राज्य आरम्भ ही से पतन का शिकार होने लगता है। जब ख़र्चे बढ़ेंगे तो बैतुल-माल पर बोझ बढ़ेगा, जब बैतुल-माल पर बोझ बढ़ेगा तो शासकों को भारी टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब भारी टैक्स लगाए जाएँगे तो जनसाधारण टैक्स देने में आना-कानी करेंगे। चुनाँचे भ्रष्टाचार के मामले सामने आएँगे। भ्रष्टाचार पैदा होगा तो शासकों को बल-प्रोयग की ज़रूरत पड़ेगी, वे बल प्रयोग करेंगे तो जनसाधारण में नफ़रत पैदा होगी, जब नफ़रत पैदा होगी तो वे जायज़ मामलात में सहयोग से भी हाथ उठा लेंगे। इस तरह राज्य में एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जो पतन और पिछड़ेपन की प्रक्रिया को तेज़ कर देगा। लेकिन अगर ऐसा न हो और राज्य बदस्तूर बेहतर अन्दाज़ में काम करता रहे, सन्तुलन की नीति अपनाए तो वह विकास की प्रक्रिया जारी रखता है और सांस्कृतिक विकास के तीसरे दर्जे में शामिल हो जाता है। जहाँ राज्य को एक बाक़ायदा और संगठित संस्था का रूप प्राप्त हो जाता है। राज्य के अलग-अलग विभाग बनते हैं। राज्य के क़ानून बहुत विस्तार से संकलित होते हैं। प्रशासनिक क़ानून सामने आता है। जीवन के विभिन्न विभागों को मज़बूत और संगठित करने के लिए राज्य की अलग-अलग संस्थाएँ बनती हैं।
यहाँ शाह साहब ने ‘सीरतुल-मुलूक’ के नाम से बादशाहों के तर्ज़े-अमल और चरित्र एवं आचरण को बयान किया है। यह बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि शाह साहब ने हर जगह ‘मलिक’ यानी बादशाह की शब्दावली प्रयोग की है। शासकों का तर्ज़े-अमल कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? शासकों को किस चीज़ से बचना चाहिए? वे इन बातों से क्यों नहीं बचते? इन बातों से बचने के लाभ क्या हैं? और न बेचने के नुक़सानात क्या हैं? यह सब कुछ शाह साहब ने ‘सीरतुल-मुलूक’ के शीर्षक से बयान किया है। फिर उन्होंने बताया कि शासकों को सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है। सहयोगी किन-किन मैदानों में होते हैं, उनकी विशिष्टताएँ क्या हैं? उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिएँ, क़ाज़ी की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? सरकारी विभाग क्या-क्या होने चाहिएँ और उनके प्रमुखों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? शहर के मेयर या प्रबन्धकों की ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिएँ? टैक्स वुसूल करनेवाले कैसे लोग होने चाहिएँ, बादशाह के सहयोगी यानी ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए। ये वे मामलात हैं जो राज्य के विकास की अनिवार्य अपेक्षा हैं।
इस तरह जब राज्य विकास के रास्ते पर चलता रहता है तो फिर वह आख़िरी दर्जा प्राप्त हो जाता है जिसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने ‘इर्तिफ़ाक़े-राबिआ’ क़रार दिया है। ऐसा मालूम होता है कि ‘इर्तिफ़ाक़े-राबिआ’ की यानी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के चौथे दर्जे की जो कैफ़ियत शाह साहब ने बयान की है वह उन्होंने सल्तनते-मुग़लिया के उत्थान काल या ख़िलाफ़ते-बनी-अब्बास के उत्थान काल को देखकर लिखी है। यह एक ऐसा राज्य है जिसका नेतृत्व एक बड़ा ख़लीफ़ा या बादशाह कर रहा है। उसके अधीन बहुत-से राज्य और हुकूमतें हैं। वहाँ की विकसित व्यवस्था पूरी तरह कार्यरत है। शरीअत के आदेशों का पालन हो रहा है। जनसाधारण को न्याय और इंसाफ़ बड़ी हद तक उपलब्ध है और वे तमाम ज़िम्मेदारियाँ अंजाम पा रही हैं जो एक आदर्श और उच्चस्तरीय राज्य में होनी चाहिएँ।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) के अलावा दूसरे बहुत-से चिन्तकों ने राज्य पर विचार व्यक्त करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों को विभिन्न ढंग से बयान किया है। बहुत-से चिन्तकों ने राज्य के अस्तित्व को एक इंसान के अस्तित्व से उपमा दी है। इस्लामी वैचारिकता के इतिहास का सबसे पहला बड़ा दार्शनिक अबू-नस्र फ़ाराबी है जिसने राजनीति को अपनी विशेष दिलचस्पी का मैदान बनाया। उसने राजनीति के विषय पर अनेक किताबें हमारे लिए छोड़ी हैं। उसने भी राज्य यानी मदीना के अस्तित्व को इंसान के शरीर से उपमा दी है। जिस तरह एक इंसानी शरीर में वह अंग जो मौलिक भूमिका निभाता है जिसकी हैसियत शरीर के राज्य में बादशाह की है, यानी दिल, वह सबसे परिपूर्ण और स्वस्थ हो तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह देश का प्रमुख अगर हर दृष्टि से परिपूर्ण हो, मानसिक, वैचारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ हो तो पूरा राज्य स्वस्थ रहता है। इसी तरह से वह आदर्श और उच्चस्तरीय राज्य जिसको फ़ाराबी ‘मदीना-ए-फ़ाज़िला’ के नाम से याद करता है, उसकी मिसाल उस परिपूर्ण और स्वस्थ मानव शरीर की है जिसके सारे अंग अपनी-अपनी जगह काम कर रहे हों। किसी अंग में कोई कमी या शिकायत न हो। और शरीर के तमाम अंग पूरे तौर पर वे कर्त्तव्य निभा रहे हों जो उन अंगों की ज़िम्मेदारी है।
इस्लामी चिन्तकों ने जहाँ राज्य से बहस की है वहाँ हुकूमत से भी बहस की है। हुकूमत के लिए मुतकल्लिमीने-इस्लाम और दार्शनिकों ने ‘इमाम’ और ‘इमामत’ की शब्दावली प्रयोग की है। ‘इमाम’ का शब्द राज्य प्रमुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन बहुत-से प्राचीन लेखों में, विशेषकर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के लेखों में ‘इमाम’ का शब्द राज्य के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। जो ज़िम्मेदारियाँ राज्य निभाता है वह मूलतः इमाम की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इमाम ही दरअस्ल ‘इमामत’ की इन ज़िम्मेदारियों का सबसे बड़ा रखवाला है, जो इस्लाम के अनुसार और इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में निभानी होती हैं। ‘इमाम’ और ‘उम्मत’ (मुस्लिम समुदाय) ये दोनों एक ही माद्दे (धातु) से निकले हैं। जैसा कि पहले विस्तार से बयान किया जा चुका है। ‘उम्मत’ का नसब यानी मुस्लिम समुदाय का गठन समष्टीय रूप से मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। मुसलमानों का सबसे मौलिक सामूहिक कर्त्तव्य यह है कि वे मुस्लिम समुदाय का गठन करें। ‘उम्मत’ की सुरक्षा के लिए इमामत का अस्तित्व अनिवार्य है। इसलिए नस्बे-इमामत की हैसियत एक महत्त्वपूर्ण फ़र्ज़े-किफ़ाया की है। यानी इस्लामी राज्य की स्थापना मुसलमानों का एक सामूहिक कर्त्तव्य है। यह फ़राइज़े-किफ़ाया पूरी ‘उम्मत’ के ज़िम्मे होते हैं। अगर ‘उम्मत’ के कुछ व्यक्ति इस फ़र्ज़ को अंजाम दे लें तो पूरी ‘उम्मत’ की ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है। और अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्ति भी इन फ़राइज़ को पूरा न करें और ये फ़राइज़ अधूरे रह जाएँ या निभाए बिना रह जाएँ तो पूरी ‘उम्मत’ उसकी ज़िम्मेदार होगी।
चूँकि मुस्लिम समुदाय की ज़िम्मेदारी है कि वह राज्य की स्थापना करे, इमाम का चुनाव करे, नेतृत्वकर्ताओं की नियुक्ति करे। इसलिए ‘उम्मत’ को इमाम को अपदस्थ करने का अधिकार भी प्राप्त है। यह बात तमाम इस्लामी चिन्तकों ने लिखी है जिसमें तमाम अहले-सुन्नत, मोतज़िला, ख़वारिज और दूसरे अनेक फ़िरक़े शामिल हैं। उनका कहना यह है कि इमामत की स्थापना का सर्वप्रथम और उच्चस्तरीय तरीक़ा यह है कि मुस्लिम समाज प्रत्यक्ष रूप से या अपने चुने हुए और श्रेष्ठ प्रतिनिधियों के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, एक व्यक्ति को नेता चुन ले और शरीअत के अनुसार स्थानीय रिवाज और ज़माने के तरीक़े को सामने रखते हुए राज्य की व्यवस्था क़ायम करे। मावर्दी ने लिखा है कि ये तमाम मुसलमानों का सामूहिक हक़ है और मुसलमानों को यह अधिकार प्राप्त है कि उस व्यक्ति को पसन्द करें, जिसके बारे में उनको यक़ीन हो कि वह नेतृत्व की तमाम अपेक्षाएँ पूरी कर सकेगा, उसको अपना नेता और प्रमुख चुन लें। फिर यह प्रमुख जिसके लिए ‘इमाम’ या ‘ख़लीफ़ा’ या ‘अमीर’ की शब्दावलियाँ प्रयोग होती रही हैं (जिसके लिए बहुत-सी दूसरी शब्दावलियाँ भी प्रयोग होती रही हैं) शेष व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। इस नियुक्ति में यह प्रमुख मुसलमानों के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करेगा।
हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक जगह फ़रमाया है कि इमामत और इमारत मुसलमानों के सामूहिक अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इमाम या अमीर नेक हो या बदकार उसका अस्तित्व बहरहाल अनिवार्य है। अमीरुल-मोमिनीन (हज़रत अली) से सवाल किया गया कि नेक और भला इमाम तो समझ में आता है, लेकिन बदकार इमाम का अस्तित्व क्यों ज़रूरी है? उन्होंने फ़रमाया, “नेता और इमाम अगर बदकार भी होगा तो कम-से-कम हदें क़ायम होती रहेंगी, रास्ते शान्तिपूर्ण रहेंगे, जिहाद की अपेक्षा पूरी की जा सकेगी। जनसाधारण के भौतिक अधिकार और आर्थिक ऋण अदा होते रहेंगे।” इसलिए अगर राज्य प्रमुख नेकी, भलाई और तक़्वा (ईशपरायणता) के उस स्तर पर नहीं है जो शरीअत को अभीष्ट है, तो भी उसका अस्तित्व बहरहाल अनिवार्य है। यहाँ यह बात विचारणीय है कि हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) जिस बदकार और दुष्कर्मी शासक के अस्तित्व की कल्पना कर रहे थे उसके बारे में भी उनको यह यक़ीन ज़रूर था कि ऐसे बदकार शासक भी, ऐसे उल्लंघनकारी शासक भी, हदें क़ायम करेंगे, रास्तों को शान्तिपूर्ण बनाएँगे। दुश्मन के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे और आम लोगों के अधिकारों का ख़याल रखेंगे। आज उनमें से शायद ही कोई ज़िम्मेदारी मुस्लिम जगत् में राज्य की ओर से अदा की जा रही हो, हदें कितनी क़ायम की जा रही हैं? रास्ते कहाँ-कहाँ और कितने शान्तिपूर्ण हैं? इस्लाम-दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद कौन कर रहा है? जनसाधारण के आर्थिक ऋण कौन चुका रहा है? ज़कात की व्यवस्था कहाँ-कहाँ क़ायम है? कितने हक़दारों को ज़कात मिल रही है? यह वाक़ई एक सवालिया निशान है जो पूरी ‘उम्मत’ के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है।
इमामत की स्थापना फ़र्ज़े-किफ़ाया है और वाजिब है। इसके लिए इस्लामी फ़ुक़हा ने बहुत-से तर्क दिए हैं। एक बड़ा तर्क जो हर जगह दिया जाता है, जो कि फ़िक़्हे-इस्लामी का सिद्धान्त है, वह यह है कि “जिस चीज़ पर किसी वाजिब के अदा किए जाने का दारोमदार हो वह चीज़ भी वाजिब होती है।” चूँकि इस्लामी क़ानून का लागू करना अनिवार्य है, एक दीनी कर्त्तव्य है और यह कर्त्तव्य राज्य के अस्तित्व के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्य का अस्तित्व भी ज़रूरी है।
इस तरह मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने अनेक मिसालें देकर यह बयान किया है कि अगर राज्य मौजूद न हो तो उसकी अनुपस्थिति से वे मुश्किलें और समस्याएँ पैदा होंगी जो हुकूमत के अस्तित्व के बिना दूर नहीं की जा सकतीं। अगर हुकूमत मौजूद होगी तो सुख-शान्ति क़ायम रहेगी। लोगों का जान-माल सुरक्षित रहेगा। अगर हुकूमत मौजूद न हो तो समाज में अराजकता होगी। क़त्लो-ग़ारत होगी। अकाल का सामना करना पड़ेगा। औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी। और हर वह व्यक्ति जो अपने गिर्द शक्ति जुटाने में सफल हो जाए वह स्थानीय शासक बन बैठेगा। लोगों के जान-माल का मालिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जनसाधारण को न ज्ञान प्राप्ति का मौक़ा मिलेगा, न सुकून से इबादत करने के लिए समय मिलेगा और बहुत-से लोग बर्बादी का शिकार हो जाएँगे। यह दलील इमाम ग़ज़ाली (रह॰) की है, इमाम ग़ज़ाली भी बुरे-से-बुरे दौर में जिन बरकतों के इच्छुक थे वे बरकतें आज मुस्लिम जगत् में लुप्त होती जा रही हैं।
मावर्दी, अबू-याला और दूसरे बहुत-से इस्लामी विद्वानों ने बार-बार यह लिखा है कि दीन (धर्म) की सुरक्षा के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। यह बात आज के सेक्युलर समाज को अजीब मालूम होगी। लेकिन सच यह है कि इस्लामी व्यवस्था में राज्य और दीन, धर्म और सल्तनत दोनों साथ-साथ चलते हैं। दोनों एक-दूसरे की पूर्ति करते हैं। दोनों एक-दूसरे के मददगार हैं। दोनों की अपेक्षाएँ एक-दूसरे से पूरी होते हैं। चुनाँचे मावर्दी ने यह बात लिखी है कि जब दीन कमज़ोर पड़ता है तो हुकूमत भी कमज़ोर हो जाती है। और जब दीन की पृष्ठपोषक हुकूमत ख़त्म होती है तो दीन भी कमज़ोर पड़ जाता है, उसके निशानात मिटने लगते हैं, उसके आदेशों में लोग रद्दो-बदल शुरू कर देते हैं और हर व्यक्ति नई-नई बिदअतें निकालने लगता है। यों होते-होते दीन के सारे लक्षण मिटने लगते हैं। अगर हुकूमत दीन का बचाव न करे और दीन की सुरक्षा न करे तो लोगों के दिल उसकी तरफ़ उन्मुख नहीं होंगे। इस हुकूमत को जनसाधारण की तरफ़ से मदद और आज्ञापालन नहीं मिलेगा। न तो वह हुकूमत क़ायम हो सकेगी जो दीन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, न अपने मामलात को साफ़ अन्दाज़ में चला सकेगी। इसके नतीजे में दमन होगा। समाज में बिखराव फैलेगा और तरह-तरह की तबाहियाँ पैदा होंगी।
अब्दुल्लाह-इब्नुल-मोतिज़ एक प्रसिद्ध साहित्यकार, शाइर और आलोचक था। एक दिन के लिए ख़लीफ़ा भी रहा। उसको एक ही दिन बाद अपदस्थ कर दिया गया था। उसने एक जगह लिखा है कि हुकूमत दीन ही की बदौलत क़ायम रह सकती है और दीन राज्य और हुकूमत ही की वजह से ताक़त पा सकता है। इस्लामी धारणा यही है कि दीन और राज्य दोनों एक-दूसरे के मददगार हों, एक-दूसरे की पूर्ति करनेवाले हों। मुसलमानों के सबसे बड़े सामूहिकता विशेषज्ञ इब्ने-ख़लदून ने भी यही बात कही है। उसने कहा है कि अगर किसी राज्य को दीनी दावत की मदद प्राप्त हो और राज्य को दीन की पुश्तपनाही प्राप्त हो तो उसकी ‘असबियत’ मज़बूत रहती है। उसका समर्थन करनेवाले इकट्ठा रहते हैं। और उनमें आपस में जो ईर्ष्या और मुक़ाबलेबाज़ी है वह ख़त्म हो जाती है। और सब मिलकर साझे दीनी उद्देश्यों और साझे सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब भी दीन की शक्ति कमज़ोर पड़ेगी तो भाषायी, क़बाइली, क्षेत्रीय और स्थानीय असबियतें जन्म लेंगी और मूल उद्देश्य से ध्यान हट जाएगा, लेकिन अगर दीनी दावत मज़बूत हो तो फिर स्थानीय असबियतें सिर नहीं उठातीं, और सबका ध्यान मूल उद्देश्य की तरफ़ लग जाता है। इब्ने-ख़लदून ने इतिहास की घटनाओं से, क़ादसिया और यरमूक की कामयाबियों से, अल्लाह को एक माननेवालों के पूरे दौर के इतिहास से यह साबित किया है कि इस्लामी इतिहास में वे राज्य सफल रहे हैं जिनके दौर में दीनी दावत मज़बूत थी। जो दीन के पाबन्द थे और दीन ही की मदद से उनको शक्ति मिल रही थी।
अगर हम इस्लामी इतिहास का जायज़ा लें तो पता चलता है कि अधिकांश बड़े-बड़े साम्राज्य धर्म ही के आधार पर, यानी इस्लाम के आधार पर ही, स्थापित हुए। यह बात इब्ने-ख़लदून ने तो कही है, लेकिन इतिहास के अवलोकन से भी यही अन्दाज़ा होता है। इस्लामी इतिहास पर हम जितना भी ग़ौर करें और बड़े-बड़े मुस्लिम राज्यों के आरम्भ का जायज़ा लें तो स्पष्ट होता है कि उनमें अधिकांश का आरम्भ दीनी उत्प्रेरकों के आधार पर हुआ है। और जब तक वे दीनी उत्प्रेरक क़ौमी रहा, राज्य क़ौमी रहा। जब दीनी उत्प्रेरक कमज़ोर हो गया राज्य की बुनियादों में कमज़ोरी के लक्षण नुमायाँ होने लगे।
इस्लाम के मुख्य दौर के इतिहास से भी यही अन्दाज़ा होता है कि ‘उम्मत’ में सबसे ज़्यादा जोशो-ख़रोश से जिस मामले पर बहस हुई, जिसके आधार पर विभिन्न मसलक अस्तित्व में आए, कलामी फ़िरक़े बने, विभिन्न मौक़ों पर जंगें भी हुईं, वह यही इमामत और राज्य की समस्या थी। इमामत और राज्य के दीनी आधार पर क़ायम होने को हर मुसलमान विचारधारा के नज़दीक सर्वसहमति प्राप्त है। इस सिद्धान्त को सब मानते हैं। वे शीया हों, अहले-सुन्नत (सुन्नी) हों, ख़वारिज हों, ज़ैदी हों, ये सब-के-सब राज्य के दीनी तसव्वुर और धार्मिक बुनियादों को मानते थे। और वैचारिक और कलामी दृष्टि से आज भी मानते हैं। इन सब कलामी मदारिस के दरमियान जो चीज़ समान रूप से पाई जाती है वह राज्य और हुकूमत का दीनी बुनियादों पर क़ायम होना है। अल्लामा शहरिस्तानी प्रसिद्ध मुतकल्लिमीने-इस्लाम में से हैं, उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा और लम्बा मतभेद जिस मामले पर रहा है वह राज्य और इमामत की समस्या है। इस्लाम के इतिहास में किसी धार्मिक मामले पर इतनी बार तलवार नहीं उठाई गई है जितनी बार इमामत और राज्य की समस्या पर उठाई गई है। इससे यह अन्दाज़ा होता है कि इस्लामी विचारधारा में राज्य का अस्तित्व किस हद तक ज़रूरी और कितना अनिवार्य समझा गया।
जैसा कि मैंने बताया, यह बात इस्लामी अक़ीदों (मान्यताओं) का हिस्सा बन गई थी और मुतकल्लिमीने-इस्लाम उसको अक़ीदे के तौर पर बयान करते थे। अक़ीदों की प्रसिद्ध किताब जो मदरसों में पढ़ाई जाती है, यानी ‘शरह अक़ाइदे-निसफ़ी’ उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों में एक ऐसे इमाम यानी राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है जो शरीअत के आदेश लागू करे, हुदूद (शरई सज़ाओं, शरई नैतिक सीमाओं) को क़ायम करे, सरहदों की रक्षा करे, फ़ौजों को तैयार रखे, ज़कात और सदक़ात की वुसूली की व्यवस्था स्थापित करे, चोरों, डाकुओं और फ़साद फैलानेवालों पर कंट्रोल करे, जुमओं और ईदों की नमाज़ों का प्रबन्ध करे, जनसाधारण के दरमियान अगर मतभेद या विवाद हों तो उनका फ़ैसला करे, सत्य और न्याय के आधार पर गवाहियाँ स्वीकार करने की व्यवस्था करे, छोटे बच्चों और बच्चियों का संरक्षण करे, जिनका कोई संरक्षक न हो उनके अधिकारों की देखभाल करे, जो नौजवान बेसहारा हैं उनकी शादियों का और दाम्पत्य जीवन का प्रबन्ध करे, ग़नीमत (युद्ध में प्राप्त माल) अगर कहीं से प्राप्त हुई है उसके वितरण का प्रबन्ध करे, और वे तमाम काम अंजाम दे जो व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकते, लेकिन जिनका शरीअत ने आदेश दिया है। हम यह कह सकते हैं कि यह इस्लामी राज्य के वे मौलिक फ़राइज़ भी हैं जो इस्लामी फ़ुक़हा ने बयान किए हैं। इन फ़राइज़ के अलावा अन्य फ़राइज़ भी बयान हुए हैं जिनके विवरण मैं अभी बयान करता हूँ।
‘इमामत’ क़ायम करने के तर्कों के सन्दर्भ में इस्लामी विद्वानों ने इजमाए-उम्मत (मुस्लिम विद्वानों की सर्वसहमति) का भी ज़िक्र किया है। इजमाए-सहाबा का भी ज़िक्र किया है। बुद्धि और इज्तिहाद के आधार पर भी तर्क दिए हैं। पवित्र क़ुरआन और हदीसों से तर्क दिए हैं, जहाँ ‘ऊलिल-अम्र’ का ज़िक्र है जहाँ ‘ऊलिल-अम्र’ के आज्ञापालन का उल्लेख है, उन आयतों और हदीसों से भी तर्क दिए हैं। शीया लोग इमामत के बारे में नस्स (क़ुरआन या हदीस के स्पष्ट आदेश) के क़ाइल हैं। उनका कहना यह है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने बाद इमाम के लिए नस्स के ज़रिए स्पष्ट कर दिया था। शेष मुसलमान इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इमामत की अनिवार्यता पर या इमामत के क़ायम होने की अनिवार्यता पर ये सब एकराय हैं। इस मामले की हद तक शीया या सुनी या अहले-सुन्नत के दूसरे गिरोहों के दरमियान कोई मतभेद नहीं है।
राज्य की स्थापना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर राज्य का अस्तित्व न हो तो जहाँ एक तरफ़ बहुत-से शरई आदेशों पर कार्यान्वयन रह जाएगा, वहाँ समाज में ऐसी अफ़रातफ़री पैदा होगी जिसमें हर व्यक्ति का जान-माल ख़तरे में पड़ जाएगा। लोगों की ज़िन्दगी मुश्किल हो जाएगी। आम लोगों के मामलात ऊहापोह के माहौल में दुरुस्त नहीं हो सकते, जब उनका कोई प्रमुख न हो। और अगर जाहिल और असभ्य लोग सरदार हो जाएँ, तो वे भी सरदार न होने के मुतरादिफ़ है। गोया अरबों में इस्लाम से तीन सौ, साढ़े तीन सौ साल पहले से यह धारणा मौजूद रही है कि किसी अफ़रातफ़री की हालत में कोई समाज अपना अस्तित्व बरक़रार नहीं रख सकता। और विकास की प्रक्रिया को, बेहतरी की प्रक्रिया को, सुधार की प्रक्रिया को राज्य प्रशासन के बिना जारी नहीं रख सकता। राज्य या राजनैतिक प्रशासन हर हाल में ज़रूरी है। अगर जाहिल, अल्पज्ञानी, कम समझ और असभ्य लोग राज्य का नेतृत्व अपना लें तो यह सामाजिक बर्बादी के समान है।
एक ज़माना था कि इस्लामी फ़ुक़हा यह बयान किया करते थे कि इस्लामी राज्य के प्रमुख के लिए मुज्तहिद होना ज़रूरी है। यानी राज्य प्रमुख न केवल आलिम हो, न केवल फ़क़ीह हो, बल्कि इतना बड़ा फ़क़ीह हो कि इज्तिहाद की क्षमता रखता हो और मुज्तहिद के पद पर आसीन हो। इस शर्त से कम-से-कम इस स्तर का अन्दाज़ा होता है कि इस्लाम के मुख्य दौर के विद्वान और चिन्तक किस स्तर का राज्य अपने ज़ेहन में रखते थे और किस स्तर का राज्य उनके ख़याल में स्तरीय इस्लामी राज्य था।
यह राज्य कैसे अस्तित्व में आएगा? इस बारे में सबका मत यह है कि यह अहले-हल्लो-अक़्द के चुनाव के द्वारा अस्तित्व में आएगा। अहले-हल्लो-अक़्द से मुराद (इस्लामी विद्वानों का) वह वर्ग है या वह गिरोह या जमाअत है जिसको जनसाधारण का विश्वास प्राप्त हो और अपने ज्ञान की दृष्टि से, अपने अनुभव और सामाजिक सम्मान की दृष्टि से, उसको जनसाधारण का प्रतिनिधि समझा जाता हो। अहले-हल्लो-अक़्द की विभिन्न परिभाषाएँ और व्याख्याएँ विभिन्न ढंग से इस्लामी विद्वानों ने की हैं। जिस ज़माने में जो लोग अहले-हल्लो-अक़्द समझे जाते थे उनको सामने रखकर अहले-हल्लो-अक़्द की परिभाषा की गई। लेकिन हर ज़माने में तीन प्रकार के लोग अहले-हल्लो-अक़्द में बहरहाल शामिल रहे। एक समाज के सबसे नुमायाँ विद्वान और बुद्धिजीवी, दूसरे विभिन्न क्षेत्रों और गिरोहों के नेता और प्रमुख, जिनमें आदिवासी प्रमुख भी शामिल हैं। इनमें विभिन्न क़ौमों और क्षेत्रों के नुमायाँ व्यक्ति भी शामिल हैं यानी आम चेहरे, और तीसरे वे लोग थे जो किसी वजह से जनसाधारण में अलग पहचान रखते थे। अपनी सेवाओं की दृष्टि से, अपनी व्यक्तिगत क्षमता की दृष्टि से, अपनी निष्ठा की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से अलग व्यक्तित्व, ये सब मिलकर अहले-हल्लो-अक़्द कहलाते थे। अहले-हल्लो-अक़्द जब किसी व्यक्ति पर मतैक्य कर लेते, या किसी की सरबराही के बारे में सर्वसहमति से फ़ैसला कर लेते तो वह व्यक्ति राज्य का प्रमुख समझा जाता था और फिर वह शरीअत के आदेशों और प्रचलित रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार शेष मामलों को चलाया करता था।
यहाँ इस मरहले पर यह बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम के इतिहास के लम्बे दौर में राज्य का संविधान अधिकांश समय एक असंकलित और अलिखित संविधान रहा है। पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल को मौलिक संवैधानिक सिद्धान्त की हैसियत प्राप्त थी। उनके बाद इस्लाम के बड़े विद्वानों के सर्वसम्मत फ़ैसले और इजमाई रायों को सनद (प्रमाण) का दर्जा प्राप्त था। इसके बाद स्थानीय परम्पराओं और क्षेत्रीय रिवाजों का दर्जा था जो हर इलाक़े और राज्य में विभिन्न होते थे। शासक इन सब मामलों की पैरवी किया करते थे और आम तौर से इस्लामी विद्वानों और फुक़हा के मश्वरे से, क़ाज़ी और मुफ़्ती लोगों की राहनुमाई में अपने फ़राइज़ (कर्त्तव्य) अंजाम दिया करते थे।
यह इस्लामी राज्य जो अहले-हल्लो-अक़्द के सर्वसम्मत फ़ैसले से क़ायम होता था, वह एक अन्तर्मानवीय राज्य था। इस दृष्टि से कि उसका आधार मात्र इंसान होने पर था। उसका आधार किसी इलाक़ाई या नस्ली या भाषायी विभाजन पर नहीं होता थी। इंसान बहैसियते-इंसान उसके नागरिक होते थे। हर वह व्यक्ति और हर वह इंसान जो इस्लामी राज्य का शहरी बनना चाहे उसका शहरी बन सकता था। इसके लिए मुसलमान होने या न होने की शर्त न थी। मुसलमान भी इस राज्य के शहरी थे। ग़ैर-मुस्लिम भी इस राज्य के बराबर के शहरी थे, बल्कि इस राज्य में ग़ैर-मुस्लिमों की सुरक्षा ज़्यादा होती थी। ग़ैर-मुस्लिमों को ख़ुसूसी छूट का हक़दार समझा जाता था। उनकी सुरक्षा राज्य अपनी विशेष ज़िम्मेदारी समझता था। राज्य के व्यक्ति इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देना अपना मौलिक कर्त्तव्य समझते थे। प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान और इस्लामी फ़ुक़हा ग़ैर-मुस्लिमों की सुरक्षा में शासकों से आगे रहते थे।
यह राज्य एक वास्तविक रिपब्लिक (republic) थी। इस दृष्टि से कि यह राज्य आम लोगों की मर्ज़ी से क़ायम होता था। अहले-हल्लो-अक़्द की रज़ामन्दी इसमें शामिल थी। जो लोग मामलात को चलाने के ज़िम्मेदार थे उनकी रज़ामन्दी और मश्वरे से ही उत्तराधिकारी की नियुक्ति होती थी। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि किसी महत्त्वपूर्ण सरकारी पद पर किसी की नियुक्ति या उत्तराधिकारी की नियुक्ति को अहले-हल्लो-अक़्द ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह राज्य सिंहासन पर न बैठ सका। ऐसा भी हुआ कि एक व्यक्ति के राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद अहले-हल्लो-अक़्द ने उससे सहमति नहीं जताई और उसको सिंहासन छोड़ना पड़ा। यक़ीनन इस परम्परा के विरुद्ध भी हुआ। यक़ीनन कुछ शासकों ने इस्लामी आदेशों का उल्लंघन भी किया। लेकिन व्यक्तिगत उल्लंघनों या व्यक्तिगत विमुखताओं की वजह से इस्लामी राज्य के पूरे इतिहास को इस्लाम से विमुख होने का इतिहास क़रार नहीं दिया जा सकता।
यह एक ऐसा राज्य था जो सामाजिक समझौते पर आधारित था। सामाजिक समझौता जिसकी पश्चिम में बहुत चर्चा है, जिसको सबसे पहले प्रस्तावित करनेवाला रूसो को बताया जाता है, पश्चिम में तो मात्र एक वैचारिक बहस है। लेकिन इस्लामी इतिहास में सामाजिक समझौता एक वास्तविकता है। मदीना मुनव्वरा में जो राज्य क़ायम हुआ वह एक समझौते के आधार पर क़ायम हुआ था। बैअते-उक़बा में जो समझौता हुआ था, और दोनों पक्षों के दरमियान विधिवत रूप से बैअत हुई थी उसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा का राज्य क़ायम हुआ था। गोया अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और मदीना मुनव्वरा के प्रतिनिधियों के दरमियान पहले एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार मदीनावासियों ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लीं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना मुनव्वरा चले गए। इसलिए यह राज्य वास्तव में सामाजिक समझौते पर आधारित राज्य था।
फिर एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इस राज्य की यह है कि यहाँ राज्य क़ानून के लिए है, न कि क़ानून राज्य के लिए। दूसरी व्यवस्थाओं और दूसरे राज्यों के इतिहास में पहले राज्य अस्तित्व में आता है। फिर राज्य को बनाने और चलाने के क़ानून की ज़रूरत पड़ती है। इस्लामी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क़ानून पहले से मौजूद है। इस क़ानून को लागू करने और इसके अनुसार ज़िन्दगी की पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य दरकार है। इस क़ानून के तक़ाज़े पूरे करने के लिए एक राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। उसके क़ानून के कुछ आदेशों पर कार्यान्वयन नहीं हो सकता जब तक राज्य अस्तित्व में न आए। इसलिए राज्य को अस्तित्व में लाना पड़ता है। इसलिए यहाँ यह तर्तीब अलग है।
इस्लामी राज्य एक एकीकृत बल यानी एक (unifying force) है। जब भी और जहाँ भी इस्लामी राज्य सही इस्लामी दिशानिर्देशों पर स्थापित हुआ। उसने स्थानीय और क्षेत्रीय पक्षपातों को ख़त्म कर दिया। इसकी सैंकड़ों मिसालें इस्लामी राज्य के इतिहास में मौजूद हैं। जब भी राज्य की इस्लामियत कमज़ोर हुई, वहाँ स्थानीय पक्षपात सिर उठाकर खड़े हो गए। यह बात बीसवीं शताब्दी में भी देखने में आई है। और अतीत की तमाम शताब्दियों में देखी जाती रही है कि अगर कोई ऐसी शक्ति रही है जिसने मुसलमानों में वहदत पैदा की, जिसने मुसलमानों को क़बीलाई, नस्ली और इलाक़ाई पक्षपातों से बुलन्द करके एक दीनी भाई-चारे की लड़ी में पिरोया तो वह मुस्लिम समाज से जुड़ाव और मुस्लिम समाज पर आधारित इस्लामी राज्य था।
इस्लामी राज्य एक दीनी राज्य है। इस अर्थ में कि वह विशुद्ध दीनी शिक्षा के आधार पर क़ायम होता है। दीनी लक्ष्य का अलमबरदार है। दीनी आदेश पर कार्यान्वयन का पाबन्द है। एक ऐसे क़ानून के लागू करने में समर्थ है जो दीनी नियमों और शिक्षाओं पर आधारित है। लेकिन दीनी राज्य होने के साथ-साथ यह राज्य पश्चिमी थ्योक्रेसी (पुरोहितवाद) की ख़राबियों और त्रुटियों से पूरे तौर पर पाक है। यहाँ न दीनदारों का कोई पैदाइशी वर्ग है, न कोई पोप है, न कोई चर्च है। न दीनदारों को कोई ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो जनसाधारण को प्राप्त नहीं हैं। यहाँ अल्लाह और बन्दे के दरमियान कोई वास्ता नहीं। अल्लाह और बन्दे के दरमियान हर वक़्त एक हॉटलाइन क़ायम है। बन्दा जब चाहे प्रत्यक्ष रूप से अल्लाह तआला से सम्पर्क कर सकता है, और अल्लाह तआला प्रत्यक्ष रूप से उसकी पुकार का जवाब देता है (यह अलग बात है कि अल्लाह का वह जवाब बन्दे को सुनाई नहीं देता) यहाँ गुनाह बख़्शवाने के लिए किसी पादरी या पुरोहित के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अल्लाह और रसूल के बाद किसी बड़े-से-बड़े आदमी की कथनी और करनी प्रमाण नहीं है। इसलिए थ्योक्रेसी की जितनी ख़राबियाँ हैं जिनकी वजह से पश्चिमवाले थ्योक्रेसी के नाम से हर समय भयभीत रहते हैं वे ख़राबियाँ इस्लामी राज्य में मौजूद नहीं हैं।
इस्लामी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन आधुनिक सेक्युलर डेमोक्रेसी की लोकतांत्रिक बुराइयों से पाक है। आज पश्चिमी लोकतंत्र ने बहुत ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं। इसलिए कि पश्चिमी लोकतंत्र ने बहुमत और अल्पमत को सत्य-असत्य का पैमाना क़रार दे दिया है। जिस तरफ़ इक्यावन (51) प्रतिशत हैं वह सत्य है। जिस तरफ़ उनचास (49) प्रतिशत हैं वह असत्य है। इस्लाम इस बहुमत एवं अल्पमत के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता। सत्य, सत्य है, चाहे सारी मानवता उसकी विरोधी हो। असत्य, असत्य है चाहे सारी दुनिया उसकी समर्थक हो। लोगों के समर्थन और विरोध से सत्य के सत्य होने में और असत्य के असत्य होने में कोई अन्तर नहीं पड़ता। सत्य वह है जो पवित्र क़ुरआन में आया है या अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान किया है। असत्य वह है जिसको शरीअत ने असत्य क़रार दिया है। इसलिए सत्य-असत्य का मापदंड वही है जो शरीअत में है। राज्य का मौलिक क़ानून वही है जो शरीअत ने बयान किया है। राज्य के उद्देश्य वही हैं जो शरीअत ने बयान किए हैं। इन सीमाओं के अन्दर कि राज्य शरीअत के वर्चस्व का ध्वजावाहक हो। शरीअत देश का सर्वोच्च क़ानून हो। इन सीमाओं के अन्दर जनसाधारण को आज़ादी है कि वे अपने प्रमुखों का चुनाव करें। इज्तिहादी मामलों में फ़ैसले करें। इज्तिहादी रायें अगर एक से अधिक हों तो उनमें से जिस राय को आम लोग अपना लें वह राय इस्लामी क़ानून है। जिन मामलों में शरीअत ने मुस्लिम समुदाय को आज़ाद छोड़ा है और वे ज़िन्दगी के अधिकांश मामले हैं। वहाँ मुस्लिम समुदाय अपने सामूहिक फ़ैसले से जिस राय को अपनाना चाहे अपना सकता है। इसलिए यहाँ लोकतंत्र की वास्तविक रूह मौजूद है।
मुसलमानों से ज़्यादा लोकतंत्र-प्रिय कौन हो सकता है? जो धर्म में भी लोकतंत्र पसन्द हैं। जिनका धर्म भी विशुद्ध लोकतांत्रिक ढंग से काम करता है। नमाज़ जैसी इबादत में इमामत करने के लिए जिसको जनसाधारण पसन्द करें वही इमामत कर सकता है। जिसको जनसाधारण ना-पसन्द करें और वह इमामत करने लगे तो उसको ना-पसन्द किया गया है। हदीस में आया है “अल्लाह तआला उस इमाम पर लानत भेजता है जो ज़बरदस्ती लोगों की इमामत करे और लोग उसे ना-पसन्द करते हों।” इसलिए लोकतंत्र की रूह तो इस्लाम की रग-रग में मौजूद है। लेकिन यह लोकतंत्र आधुनिक अधार्मिक डेमोक्रेसी की ख़राबियों से पूरे तौर पर पाक है।
इस्लामी राज्य में क़ानून का पूर्ण और वास्तविक राज्य वह गुण है जिससे इस्लामी राज्य शेष तमाम राज्यों से अलग होता है। यहाँ क़ानूनसाज़ी भी आज़ाद है। शासकों के प्रभाव एवं पहुँच से परे है। शासक भी क़ानून का उसी तरह पाबन्द है जिस तरह जनसाधारण पाबन्द हैं। जिन अदालतों के सामने जनसाधारण पेश होते हैं, उन्हीं अदालतों के सामने ख़ुलफ़ा भी पेश होते हैं। जिस तरह जनसाधारण क़ानूनों के पाबन्द हैं इसी तरह शासक गण भी पाबन्द हैं। अगर जनसाधारण का दावा रद्द किया जा सकता है तो हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) का दावा भी रद्द किया जा सकता है। अगर जनसाधारण क़ाज़ी के यहाँ पेश होते हैं तो हज़रत उमर-बिन-ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अन्हु) भी क़ाज़ी के सामने पेश होते हैं।
इस्लामी राज्य का संविधान, जैसा कि मैंने बताया, एक असंकलित और अलिखित संविधान रहा है। अलबत्ता विभिन्न समयों में शासकों ने इन संवैधानिक परम्पराओं को और शरीअत से सम्बन्धित आदेशों को दस्तावेज़ के रूप में भी तैयार किया। ऐसी मिसालें अतीत में मौजूद हैं जिनको ‘दस्तूरुल-अमल’ के नाम से याद किया गया। भारत में अनेक दस्तावेज़ात तैयार की गईं जिनको एक लिखित और संकलित संविधान की रूपरेखा क़रार दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर इस्लामी इतिहास में संविधान असंकलित रहा है। उसकी मौलिक धारणाओं में जो सिद्धान्त शामिल थे उनमें सबसे पहला सिद्धान्त शरीअत के वर्चस्व का सिद्धान्त था, यानी यह बात कि अल्लाह तआला की शरीअत सर्वोच्च क़ानून है। और राज्य में जारी होनेवाले तमाम नियम और क़ानून, शासकों के आदेश, सब शरीअत की सीमाओं के पाबन्द हैं।
अल्लाह का हाकिम होना एक ऐसा सिद्धान्त है जिसको आज कुछ आधुनिक लेखकों ने हाकिमियत या Sovereignty के नाम से याद किया है। यह शब्दावली अगरचे नई है, लेकिन यह कल्पना या नज़रिया शुरू से चला आ रहा है। तमाम उलमाए-उसूल ने इसको बयान किया है कि आदेश दरअस्ल अल्लाह तआला का है। और वास्तविक शासक दरअस्ल अल्लाह तआला है। बन्दों की हैसियत उत्तराधिकारियों की है। वे यहाँ उत्तराधिकारी की हैसियत रखते हैं। अस्ल मालिक और अस्ल शासक अल्लाह तआला है। लोकतंत्र का शासनाधिकार ऐसी सामूहिक ख़िलाफ़त की अनिवार्य अपेक्षा है।
लोकतंत्र के शासनाधिकार और सामूहिक उत्तराधिकार का अनिवार्य नतीजा है कि राज्य में शूरा के सिद्धान्त पर कार्यान्वयन किया जाए। मामलात का फ़ैसला आपसी मश्वरे से किया जाए। जिन मामलों में शरीअत ने स्पष्ट रूप से आदेश दे दिए हैं उन आदेशों में तो किसी मश्वरे की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन आदेशों पर कार्यान्वयन के लिए क्या-किया जाए? कैसे, और कब व्यावहारिक क़दम उठाए जाएँ? अगर किसी आदेश पर एक से अधिक तरीक़ों से अमल सम्भव हो तो किसी एक तरीक़े का चुनाव मश्वरे के आधार पर होना चाहिए। जिन मामलात में शरीअत ने आज़ाद छोड़ा है जो अधिकांश प्रशासनिक प्रकार के मामलात हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय प्रकार के मामलों से सम्बन्धित हैं, वे आपसी मश्वरे से ही तय होंगे।
चूँकि जनसाधारण क़ानून की नज़र में बराबर हैं, इसलिए ‘अद्ल’ का सिद्धान्त अनिवार्य है। पवित्र क़ुरआन ने एक जगह बयान किया है जिसका हवाला मैं पहले भी दे चुका हूँ कि अल्लाह तआला ने सारी आसमानी किताबें और शरीअतें इसी लिए उतारी हैं कि जनसाधारण में मुकम्मल न्याय और इंसाफ़ क़ायम हो जाए।
‘अद्ल’ और इंसाफ़ के साथ समता अनिवार्य है। समता होगी तो न्याय और इंसाफ़ होगा। ‘अद्ल’ और इंसाफ़ नहीं होगा तो समता भी नहीं होगी, समता नहीं होगी तो ‘अद्ल’ भी नहीं हो सकेगा। अत: ‘अद्ल’ के लिए समता का होना अनिवार्य है। इस्लाम में ‘अद्ल’ और समता साथ-साथ चलते हैं, ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ‘ऊलुल-अम्र’ का आज्ञापालन पवित्र क़ुरआन का आदेश है। ‘ऊलुल-अम्र’ से अभिप्रेत वे सब लोग हैं जो किसी-न-किसी सतह पर फ़ैसला करनेवाले हैं। ‘ऊलुल-अम्र’ में केवल शासक शामिल नहीं होते, बल्कि वे तमाम व्यक्ति और शख़्सियतें शामिल होती हैं जो किसी-न-किसी हैसियत में किसी-न-किसी सतह पर फ़ैसले करने की अधिकारी, सक्षम या पाबन्द हैं। घर में माँ-बाप हैं। घर से बाहर विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख हैं। विभिन्न संगठनों के प्रमुख हैं। इस तरह दर्जा-ब-दर्जा ‘ऊलुल-अम्र’ की हैसियत फैलती जाती है। कार्य-क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है और आख़िरकार शासक या प्रमुख राज्य पर यह सिलसिला ख़त्म होता है। लेकिन ‘ऊलुल-अम्र’ का आज्ञापालन शर्त के साथ जुड़ा है, बल्कि दो शर्तों से जुड़ा है। एक शर्त तो वह है जो पवित्र क़ुरआन और हदीस में आती है कि “अल्लाह तआला की नाफ़रमानी में किसी का आज्ञापालन नहीं किया जाएगा।” दूसरी शर्त एहतिसाब (पूछ-गछ) की है कि पूछ-गछ हर शासक से होगी। पूछ-गछ हर व्यक्ति की होगा। शासकों की भी होगी। जनसाधारण की भी होगी। प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों और फ़ुक़हा की भी होगी। क़ाज़ियों की भी होगी। दीनी शख़्सियतों की भी होगी। पूछ-गछ से परे कोई नहीं।
फिर क़ानूनसाज़ी और शासकों के कार्यों और अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित हैं। शासकों को शरई राजनीति के अनुसार निस्सन्देह विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इन अधिकारों की हदबन्दी भी शरीअत के आदेशों और क़ानून के अनुसार की गई है। ये वे मौलिक धारणाएँ हैं जिनके आधार पर इस्लामी संविधान का गठन होता है और राज्य की कार्यकुशलता संगठित होती है। राज्य की ज़िम्मेदारी दीनी (धार्मिक) भी है और सांसारिक भी, इसलिए यह एक सेक्युलर राज्य नहीं है। यहाँ धर्म और राज्य में भेद करने की कोई कल्पना नहीं है, यह राज्य इस्लाम धर्म के आधार पर क़ायम है और इस्लाम धर्म के ही विकास और निर्माण के लिए प्रयासरत और कार्यरत है। इस राज्य की ज़िम्मेदारियों में आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। शैक्षिक ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि नैतिकता और आध्यात्मिकता के मामले में यह राज्य निष्पक्ष नहीं है।
यह तथाकथित निष्पक्षता और नैतिकता तथा दीन (धर्म) से दूरी, ये सेक्युलरिज़्म के प्रभाव हैं। जो राज्य सेक्युलरिज़्म के इनकार के आधार पर क़ायम किया गया हो। वह नैतिक सिद्धान्त का ध्वजावाहक हुए बिना नहीं रह सकता। वह दीनी ज़िम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकता। इस्लामी राज्य की परिभाषा के सन्दर्भ में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने लिखा है कि इस्लामी राज्य वह है जो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के उत्तराधिकार में दीन की सुरक्षा और शरई क़ानूनों के लागू करने तथा सांसारिक मामलों की सुरक्षा के लिए क़ायम किया गया हो। ‘हिरासतुद्दीन’ और ‘सियासतुद्दुनिया’ ये शब्दावलियाँ कई इस्लामी फ़ुक़हा ने प्रयुक्त की हैं। गोया दीन की सुरक्षा, शरीअत के आदेशों का लागू करना, और सांसारिक मामलों का उपाय, यह राज्य की मौलिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसलिए इस्लामी विद्वानों ने विशेषकर और मुस्लिम समुदाय ने आम तौर से ‘इमारते-इस्तीला’ को स्वीकार किया। इमारते-इस्तीला से मुराद वह नेतृत्व है जो मात्र शक्ति के आधार पर क़ायम हुआ हो।
अगर किसी व्यक्ति ने शक्ति प्राप्त करके अपने आस-पास फ़ौज इकट्ठी करके राज्य पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने को शासक क़रार दे दिया। अब अगर वह शरीअत के आदेश लागू कर रहा है, दीन की सुरक्षा कर रहा है, सांसारिक मामलों का प्रबन्धन और प्रशासन ठीक चला रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेनेवाला शासक जायज़ शासक स्वीकार किया जाएगा अगर वह शरीअत के वर्चस्व को मानता हो, शरीअत के आदेशों पर अमल करता हो और शरीअत के क़ानूनों को लागू करने के लिए तैयार हो। यह बात तमाम इस्लामी फ़ुक़हा ने लिखी है। इसलिए कि अगर कोई ज़बरदस्ती क़ाबिज़ होनेवाला शासक शरीअत के आदेश लागू करता हो, हदें क़ायम करता हो, देश की रक्षा करता हो, लोगों की इज़्ज़त-आबरू का रक्षक हो, इस्लाम-दुश्मनों से जिहाद के लिए फ़ौजें तैयार रखता हो। ज़कात और सदक़ात की व्यवस्था क़ायम करता हो। अदालतें आज़ादी से काम कर रही हों, जुमा, ईदैन और नमाज़ों की व्यवस्था क़ायम हो, मज़लूम को इंसाफ़ मिल रहा हो, ज़ालिम को ज़ुल्म से रोका जा रहा हो। अदालतें और दूसरी संस्थाएँ काम कर रही हों। दुनिया के विभिन्न भागों में इस्लाम के आवाहक और क़ुरआन का पाठ करनेवाले (क़ारी) भेजे जा रहे हों तो फिर वह राज्य जायज़ राज्य माना जाएगा। ये तमाम फ़राइज़ (कर्त्तव्य) जो मैंने अभी बयान किए वे हैं जो अल्लामा शहरिस्तानी ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘निहायतुल-इक़दाम फ़ी इल्मुल-कलाम’ में बयान किए हैं।
गोया राज्य की यह ज़िम्मेदारी भी थी कि वह इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए जगह-जगह प्रचारक भेजे। पवित्र क़ुरआन की शिक्षा को आम करने के लिए क़ारियों की नियुक्ति करे। इस बात को निश्चित बनाए कि पवित्र क़ुरआन की शिक्षा दी जा रही है। ये तमाम कर्त्तव्य फ़िक़्हे-इस्लामी में पवित्र क़ुरआन की इस आयत से लिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि “अगर हम ईमानवालों को ज़मीन में सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज़ की व्यवस्था क़ायम करेंगे, ज़कात की व्यवस्था क़ायम करेंगे, शरीअत द्वारा भले ठहारए गए कामों (मारूफ़ात) का आदेश देंगे और शरीअत के मना किए हुए कामों (मुनकरात) को रोकेंगे।” ये चार फ़राइज़ बहुत आम प्रकार के हैं। और उनमें वे तमाम फ़राइज़ (कर्त्तव्य) शामिल हैं, वे तमाम ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं जो इस्लामी राज्य पूरा करता है। इनको इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) और मुतकल्लिमीन ने बहुत स्पष्ट रूप से बयान किया है।
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि इस्लाम के संवैधानिक और फ़िक़ही इतिहास के हर दौर में ऊलुल-अम्र की विशेषताओं का ज़िक्र किया गया है। यह स्पष्ट किया गया जो लोग शासन के पद पर आसीन हों या राज्य की संस्थाओं को चलाने के लिए नियुक्त किए गए हों, उनकी विशेषताएँ और योग्यता क्या होनी चाहिए। वे विशेषताएँ और योग्यताएँ इन्हीं कर्त्तव्यों की रौशनी में निर्धारित की जाएँगी। ज़ाहिर है महत्त्व का निर्धारण कर्त्तव्यों के निर्धारण के बाद किया जाता है। अगर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य यह है कि लोगों के स्वास्थ्य का ख़याल रखे, लोगों की बीमारियों का इलाज करे उसकी योग्यता और होगी। अगर कर्त्तव्य यह हो कि घर की चौकीदारी करे और चोरों और डाकुओं को घर में दाख़िल होने से रोके, उसके महत्त्व का निर्धारण किसी और अन्दाज़ से होगा। अगर कर्त्तव्य यह हो कि लोगों को क़ानून की शिक्षा दे, क़ुरआन की शिक्षा दे, उसकी योग्यता का निर्धारण और अन्दाज़ से होगा। इसलिए योग्यता के निर्धारण में इन चारों फ़राइज़ को जो पवित्र क़ुरआन की इस आयत में बयान हुए हैं हमेशा सामने रखा गया।
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि नमाज़ जो इबादतों का सबसे मौलिक शीर्षक है, सर्वप्रथम और मौलिक इबादत है, उसको राज्य का सबसे पहला कर्त्तव्य क़रार दिया गया है। यहाँ अधार्मिकता और सेक्युलरिज़्म की जड़ कट जाती है। इसलिए कि हुकूमत के सबसे महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्यों में से नमाज़ क़ायम करना भी है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक बार अपने तमाम गवर्नरों को लिखा था कि आप लोगों के फ़राइज़ में से सबसे महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य मेरे नज़दीक नमाज़ क़ायम करना है। यही वजह है कि उस ज़माने में फ़ौज के प्रमुख ही नमाज़ के इमाम होते थे। जो नमाज़ का इमाम होता था, वह फ़ौज का इमाम भी होता था। हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का चुनाव जब ख़िलाफ़त के लिए होने लगा तो प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने सर्वसम्मत रूप से उनकी नमाज़ की इमामत को राज्य के नेतृत्व का आधार क़रार दिया और कहा “जिस व्यक्ति को हमारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने दीन की सबसे बड़ी इबादत के लिए चुना कि वह हमारी इमामत करे, हम उनको सांसारिक मामलात में भी अपनी इमामत के लिए चुनेंगे।” इसलिए अगर राज्य प्रमुख नमाज़ की इमामत के योग्य होगा, तो ज़ाहिर है नमाज़ के इमाम के लिए जो अनिवार्य विशेषताएँ होनी चाहीएँ, वे उसमें पाई जानी चाहिएँ। यह वह कम-से-कम योग्यता है जो इस्लामी राज्य के प्रमुख में पाई जानी चाहिए, कम-से-कम नमाज़ पढ़ना जानता हो। इतना क़ुरआन जानता हो कि नमाज़ अदा कर सके। नमाज़ के आदेशों से परिचित हो। जिसने सिरे से कभी ज़िन्दगी में नमाज़ न पढ़ी हो, जो सिरे से नमाज़ पढ़ना ही न जानता हो, वह इस्लामी राज्य का प्रमुख हो जाए यह बात इस्लामी नैतिक मापदंड और इस्लामी राजनीति के अनुसार अकल्पनीय है।
इन तमाम कर्त्तव्यों और विशिष्टताओं से पता चलता है कि दीन और राजनीति का इस्लाम के अनुसार आपस में अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है। अल्लामा इक़बाल ने अपने लेखों में जगह-जगह इस सम्बन्ध को बहुत अधिक और तफ़सील से बयान किया है। और यह भी बताया है कि पश्चिम में यह सम्बन्ध क्यों असफल हुआ, उनके विचार से जब से गिरिजा व्यवस्था में रहबानियत (संन्यास) दाख़िल हुई उस समय से दीन और राज्य में भेद का कार्य शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि चूँकि कलीसा या चर्च का आधार रहबानियत थी इसलिए इस फ़क़ीरी में अमीरी समा नहीं सकती थी। इसलिए कि सुल्तानी और रहबानी में टकराव, बल्कि दुश्मनी है। एक सिर ऊँचा करती है एक सिर झुकाती है। इसलिए राजनीति ने धर्म से पीछा छुड़ा लिया, और जब दीन-दौलत में जुदाई हुई उसी लम्हे हवस की अमीरी भी शुरू हो गई। हवस की वज़ीरी भी शुरू हो गई।
यह राज्य मुस्लिम समाज के लिए विशेष रूप से और पूरी मानवता के लिए आम तौर से एक रहमत की हैसियत रखता है। अगर यह राज्य और स्तरीय समाज क़ायम हो तो वह पूरी मानवता के लिए बरकत और रहमत साबित होता है। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने विभिन्न हदीसों में इस बेहतरीन और स्तरीय राज्य की झलकियाँ बयान की हैं। एक प्रसिद्ध रिवायत में जिसको इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “जब तक तुम्हारे पेशवा और शासक तुममें बेहतरीन लोग हों, जब तक तुम्हारे दौलतमंद लोग सबसे ज़्यादा दानशील और खुले दिल के हों, और तुम्हारे मामलात आपस में मश्वरे से तय पा रहे हों तो ज़मीन की पीठ तुम्हारे लिए ज़मीन के पेट से बेहतर है।” गोया ऐसी स्थिति में तुम्हारी ज़िन्दगी एक स्तरीय ज़िन्दगी होगी। और ज़मीन की पीठ तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगी। एक और हदीस में जिसको इमाम मुस्लिम ने बयान किया है, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “तुम्हारे बेहतरीन प्रमुख और इमाम वे हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और वे तुमसे मुहब्बत करते हों, जो तुम्हारे लिए दुआएँ करते हों और तुम उनके लिए दुआएँ करते हो। और तुम्हारे बदतरीन पेशवा और इमाम वे हैं जिनसे तुम नफ़रत करो और वे तुमसे नफ़रत करें। जिनपर तुम लानतें भेजो और वे तुमपर लानतें भेजें।” दूसरे शब्दों में एक आदर्श और स्तरीय समाज में शासकों और आम लोगों के सम्बन्ध आपसी प्रेम, निष्ठा और शुभचिन्ता के होते हैं। अगर शासक और जनता दोनों एक-दूसरे के हितैषी और एक-दूसरे से प्रेम करनेवाले हैं तो गोया एक मिसाली समाज की झलक वहाँ मौजूद है। लेकिन अगर शासक और जनता के दरमियान सम्बन्ध नफ़रत का हो और एक-दूसरे को ना-पसन्द करने का हो, एक-दूसरे पर लानत भेजने का हो तो यह मुस्लिम समुदाय के पतन का प्रतीक है। मुस्लिम समाज को जल्द-से-जल्द उसका हल निकालना चाहिए। इसलिए कि जो शासक मुस्लिम समुदाय में प्रतिष्ठित होगा और जनसाधारण उसका सम्मान करते होंगे, उससे प्रेम करते होंगे, वही शासक होगा जो उनकी धारणाओं और आइडियल्ज़ के अनुसार होगा। ऐसा शासक ‘इमामे-आदिल’ की शब्दावली से याद किया गया। यानी वह इमाम और पेशवा जो न्यायप्रिय हो और ‘अद्ल’ (न्याय) करनेवाला हो। एक प्रसिद्ध मुस्लिम चिन्तक ने ‘अद्ल’ की तारीफ़ करते हुए कहा है कि ‘अद्ल’ से मुराद अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का आदेश लागू करना है।
जब अल्लाह तआला की ज़मीन में न्यायप्रिय शासक मौजूद हो तो वहाँ ख़ुद-ब-ख़ुद ‘अद्ल’ क़ायम होगा। अत: न्यायप्रिय शासक से मुराद वह व्यक्ति है जो ख़ुद भी न्याय और इंसाफ़ की अपेक्षाओं का पालन करता हो और दूसरों के साथ भी ‘अद्ल’ करता हो। ख़ुद भी शरीअत का अनुयायी हो और दूसरों को भी शरीअत की पैरवी के लिए आमादा करता हो और उसके लिए संसाधन उपलब्ध करता हो। ऐसे शासक का अस्तित्व इंसानियत के लिए बरकत है। एक प्रसिद्ध हदीस में आया है कि अगर इमामे-आदिल किसी क़ौम को नसीब हो जाए और वह एक दिन न्याय और इंसाफ़ करे तो यह कई वर्षों की इबादत से अफ़ज़ल (बढ़कर) है। एक और जगह आया है कि साठ साल की इबादत से अफ़ज़ल है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन जब लोग परेशान होंगे, और नफ़्सा-नफ़्सी (आपा-धापी) की कैफ़ियत में होंगे, तो अल्लाह तआला जिन सात प्रकार के इंसानों को अपने अर्श की छाँव में जगह देगा उनमें सबसे पहला दर्जा इमामे-आदिल का है।
इमामे-आदिल का सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि वह न्याय और इंसाफ़ क़ायम करे। न्याय और इंसाफ़ की स्थापना इस्लामी राज्य की सबसे बड़ी, सबसे मौलिक ज़िम्मेदारी है। ‘अद्ल’ का अर्थ इस्लाम में बहुत आसान और व्यापक है। इसका उल्लेख किसी हद तक पहले भी किया जा चुका है। पवित्र क़ुरआन में जहाँ हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) को ख़िलाफ़त प्रदान करने का उल्लेख है वहाँ पहला कर्त्तव्य यह बयान किया गया है कि चूँकि तुम्हें ख़लीफ़ा बनाया गया है अत: तुम इंसानों के दरमियान सत्य के अनुसार फ़ैसले करो, न्याय और इंसाफ़ से काम लो। न्याय और इंसाफ़ अदालती फ़ैसलों के ज़रिये भी होता है, न्याय और इंसाफ़ प्रशासनिक मामलों में भी होता है, धन के वितरण में भी होता है। न्याय और इंसाफ़ समाज और अर्थव्यवस्था में भी होता है। हर प्रकार का ‘अद्ल’ और इंसाफ़ क़ायम करना इस्लामी राज्य की मौलिक ज़िम्मेदारी है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जहाँ इस्लामी राज्य को बतौर एक आदर्श राज्य और एक उच्चस्तरीय राज्य बयान किया गया है वहाँ न्याय और इंसाफ़ तथा नैतिक मामलों को मौलिक महत्त्व दिया है। अबू-नस्र फ़ाराबी ने राज्य के चार प्रकार बताए हैं और हर प्रकार के लिए विशुद्ध इस्लामी और क़ुरआनी शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं। इन प्रकारों में सबसे उच्च और सबसे श्रेष्ठ प्रकार ‘मदीना-ए-फ़ाज़िला’ है जो आदर्श और स्तरीय राज्य है। इस आदर्श और स्तरीय राज्य के अलावा जितने भी प्रकार के चार राज्य हैं उन सबके लिए उसने यह शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं।
- मदीना-ए-जाहिला यानी जाहिलियत पर आधारित राज्य
- मदीना-ए-फ़ासिक़ा यानी अल्लाह के आदेशों के उल्लंघन की दावत देनेवाला और बुराई का ध्वजावाहक राज्य
- मदीना-ए-ज़ाल्ला यानी गुमराह राज्य
- मदीना-ए-मुतबद्दिला यानी दीनी मामलात और ‘अद्ल’ और इंसाफ़ के तक़ाज़ों में परिवर्तन करनेवाला राज्य
ये सब क़िस्में मदीना-ए-फ़ाज़िला यानी स्तरीय और इस्लामी राज्य का प्रतिबिम्ब हैं। यानी आदर्श और स्तरीय इस्लामी राज्य अबू-नस्र फ़ाराबी की नज़र में वह है जो नैतिक गुणों से विभूषित हो और जिसके शासक में नैतिक गुण भरपूर तरीक़े से पाए जाते हों और वह तत्त्वदर्शिता और बुद्धिमानी से काम लेता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीअत का जानकार हो, शरीअत की सुरक्षा करनेवाला, सुन्नत का आलिम और सुन्नत की सुरक्षा करनेवाला हो। गोया स्तरीय इस्लामी राज्य या मदीना-ए-फ़ाज़िला की वास्तविकता में यह बात शामिल है कि वहाँ के व्यक्ति और शासक नैतिकता और तत्त्वदर्शिता के गुणों से विभूषित हों और सुन्नतों के जानकार और रक्षक हों। अगर ऐसा होगा तो वह राज्य एक इस्लामी राज्य होगा। ऐसा नहीं होगा तो वह इस्लामी राज्य नहीं होगा।
जिस राज्य को फ़ाराबी ‘मदीना-ए-जाहिला’ कहता है, यानी जाहिलियत पर आधारित राज्य, उस की भी ऐसी बहुत-सी क़िस्में बताई जाती हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सब क़िस्में आज की दुनिया में मौजूद हैं। एक प्रकार वह बताता है मदीना-ए-ज़रूरिया, यानी वह राज्य जिसको केवल मौलिक भौतिक आवश्यकताएँ उपलब्ध करने से दिलचस्पी हो, जिसका लक्ष्य केवल यह हो कि लोगों को मौलिक आवश्यकताओं यानी रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध हो जाएँ यह मदीना-ए-जाहिला का एक प्रकार है। दूसरे प्रकार को मदीना-ए-बद्दाला कहा जाता है। यह पहले प्रकार से ज़रा ऊँचा है। यह वह राज्य है जहाँ केवल भौतिक सुविधाओं के लिए सहयोग होता है। एक राज्य वह है जिसको वह ‘मदीना-ए-अल-ख़स्सः वस-सुक़ूत’ यानी अत्यन्त कंजूस और विश्वास के अयोग्य राज्य, यह वह राज्य है जिसको सिर्फ़ शारीरिक लज़्ज़तों और ग़ैर-संजीदा व्यस्तताओं से दिलचस्पी हो। आज दुनिया के कितने देश हैं विशेष रूप से पश्चिम में, वे इसी लिए प्रसिद्ध हैं कि वहाँ शारीरिक लज़्ज़तों और ग़ैर-संजीदा हरकतों के सब संसाधन उपलब्ध हैं। और शायद इसी लिए बेकार और फ़ालतू लोग वहाँ बहुत अधिक जाते हैं। इसी मदीना-ए-जाहिला की एक क़िस्म है मदीना-ए-करामा, जिसके लोगों का वाहिद लक्ष्य यह है कि वे लोगों में प्रतिष्ठित क़रार पाएँ, लोग उनका सम्मान करें, एक और क़िस्म मदीना-ए-तग़ल्लुब है जहाँ के लोग दूसरों पर वर्चस्व पाने की कोशिश में रहते हैं। उनका मौलिक लक्ष्य केवल यह है कि दुनिया हमारे अधीन हो जाए, हमें दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाए। एक और क़िस्म मदीना-ए-जिमाइया है जिसको हम कह सकते हैं कि वह पूरी तरह स्वच्छन्द समाज है। जहाँ कोई क़ानून, नैतिकता और शरीअत मौजूद न हो और लोग हर क़ैद और नैतिकता से आज़ाद हों।
आप देख लीजिए कि ये गुण अब किन राज्यों में पाए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुस्लिम राज्य अपनी बहुत-सी कमज़ोरियों और महरूमियों के बावजूद आज भी इन ख़राबियों से बहुत हद तक पाक हैं। फ़ाराबी के नज़दीक जिस समाज के लोगों को केवल शारीरिक स्वास्थ्य से दिलचपसी हो, जिनको केवल धन की प्राप्ति से मतलब हो और शारीरिक आनन्दों से ग़रज़ हो वहाँ इच्छाओं और वासनाओं ही का राज होगा। इसलिए कि यही चीज़ें जाहिलियतवालों के नज़दीक ‘सआदत’ की हैसियत रखती हैं।
फ़ाराबी ने एक आदर्श इस्लामी राज्य के सबसे बड़े सरदार या पहले प्रमुख यानी रईसे-अव्वल का जो स्पष्टीकरण किया है वह इस ढंग से किया है कि मदीना मुनव्वरा का नबवी राज्य भी इसमें शामिल हो जाए। रईसे-अव्वल से इसका उद्देश्य सम्भवतः नबी की कल्पना अपनी राजनैतिक सोच में समोना है। वह कहता है कि रईसे-अव्वल जो किसी मदीना-ए-फ़ाज़िला का प्रमुख होता है। यह वह व्यक्ति होता है जो नैतिकता के अत्यन्त उच्च पद पर आसीन हो, वह ऐसा व्यक्ति हो कि अल्लाह की वह्य (प्रकाशना) भी उसपर अवतरित हो सकती हो। यह रईसे-अव्वल ज्ञान एवं तत्त्वदर्शिता में दूसरे इंसानों का मुहताज नहीं होता। यह ज्ञान एवं तत्त्वदर्शिता प्रत्यक्ष रूप से वह्य के द्वारा प्राप्त करता है और उस ज्ञान एवं तत्त्वदर्शिता के आधार पर अपनी व्यवस्था को चलाता है। जो लोग उस रईसे-अव्वल की प्रमुखता में जी रहे हों वे ख़ुद भी ज्ञान और तत्त्वदर्शिता तथा नैतिकता के उच्च पद पर होते हैं। वे राज्य के बेहतरीन व्यक्ति होते हैं, ‘सआदत’ (सौभाग्य) के आला दर्जे पर आसीन होते हैं। यही मुस्लिम समुदाय वह मुस्लिम समुदाय है जो उम्मते-फ़ाज़िला कहलाने का हक़दार है। जो उम्मत या क़ौम मदीना-ए-फ़ाज़िला में रहेगी वह क़ौम या उम्मत भी फ़ाज़िला होगी। ऐसा मालूम होता है कि मदीना-ए-फ़ाज़िला का विवरण बयान करते हुए फ़ाराबी के ज़ेहन में मदीना मुनव्वरा का राज्य था और उम्मत से मुराद प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की उम्मत थी।
इस्लामी शोधकर्ताओं ने राज्य के केवल वैचारिक पहलू ही से बहस नहीं की, बल्कि प्रशासनिक पहलुओं के साथ भी बहुत विस्तार के साथ चर्चा की है। शहरों की आबादी कैसे क़ायम की जाए? शहर बसाए कैसे जाएँ? आवश्यकताएँ कौन-कौन-सी हों? इनपर विद्वानों ने हर दौर में चर्चा की है। मुसलमानों ने कूफ़ा, बस्रा, कैरुआन (Kairouan), मंसूरा, क़ाहिरा, फ़ुस्तात और दूसरे बहुत-से शहर बसाए। इन सबमें नागरिक सुनियोजन की एक ख़ास परिकल्पना पाई जाती थी जिसके अनुसार ये सब शहर बसाए गए थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जब कूफ़ा और बस्रा बसाने का निर्देश दिया तो उन्होंने ज़मीन पर छड़ी से एक ऐसा नक़्शा बनाया जिसके अनुसार कूफ़ा शहर बसाया गया। और सच्चाई यह है कि नागिरक योजना में इससे सादा, इससे ज़्यादा आरामदेह और लाभदायक रूपरेखा शायद ही कोई बना पाया हो। उन्होंने फ़रमाया कि सबसे पहले एक जगह को शहर का केन्द्र क़रार दिया जाए। वहाँ शहर की जामा मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद के चारों तरफ़ खुला मैदान हो जहाँ मुसलमानों के जमा होने की जगह हो। इस मैदान के चारों तरफ़ बाज़ार हों, चारों तरफ़ चार सड़कें निकल रही हों और वे चारों सड़कें चार छोटे-छोटे केन्द्रों पर जाकर ख़त्म होती हों। इन चारों केन्द्रों को इस तरह बनाया जाए जैसे बड़े केन्द्र को बनाया जाए। गोया आज ताज़ा-तरीन नागरिक योजना के जो नक़्शे प्रचलित हैं, वे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के नक़्शे के अनुसार हैं।
इस्लामी विद्वानों ने बाह्य रूप से योजनाओं और नक़्शों के अलावा इससे भी बहस की कि राज्यों का पतन कैसे होता है? यह बात इमाम ग़ज़ाली, अल्लामा इब्ने-तैमिया, इब्ने-ख़लदून से लेकर शाह वलीउल्लाह तक सबने कही है। टैक्सों की ज़्यादती और ज़ुल्म, न्याय और इंसाफ़ न होना राज्यों के पतन का एक बड़ा कारण होते हैं। इब्ने-ख़लदून ने लिखा है कि ज़ुल्म की एक बड़ी क़िस्म यह है कि जनसाधारण के धन-दौलत पर राज्य हावी हो जाए। जिसको आज नेशनलाइज़ेशन कहते हैं, जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के कगार पर ला खड़ा कर दिया है, यह बहुत बड़ा ज़ुल्म है। लोगों की दौलत को मामूली क़ीमत पर कौड़ियों के मोल ख़रीदकर सरकारी निगरानी के नाम पर कुछ अधिकारियों के क़ब्ज़े में दे देना यह जनसाधारण के साथ बहुत बड़ा ज़ुल्म है। इसका नतीजा हुकूमत के पतन और देश की कमज़ोरी के रूप में निकलता है। इब्ने-ख़लदून ने यह भी लिखा है कि अगर शासक व्यापार करने लगें और अपने कारोबार स्थापित करने लगें तो यह जनसाधारण के लिए बहुत नुक़सानदेह होता है। इससे टैक्सों की वुसूली में ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इतिहास ने यह साबित किया कि इब्ने-ख़लदून की यह राय बहुत बारीक और गहरी नज़र पर आधारित है। जब शासक व्यापार करना शुरू कर दें और अपने कारोबार क़ायम करने लगें, शासकों की औलाद कारख़ाने बनाने लगे तो यह जनसाधारण के लिए अत्यन्त नुक़सान का कारण होता है। इसके नतीजे में सरकारी खज़ाने में संसाधनों का अभाव हो जाता है, और टैक्सों की वुसूली में अत्यन्त कमी आ जाती है। इसी तरह इब्ने-ख़लदून ने यह भी लिखा है कि जब ख़र्चों में ग़ैर-ज़रूरी वृद्धि होती है, तो टैक्सों में भी वृद्धि करनी पड़ती है। टैक्सों में वृद्धि की जाए तो व्यापार में कमज़ोरी पैदा होती है। व्यापार में कमज़ोरी आती है तो मंदी आती है। मंदी आती है तो बसावट में ख़लल पड़ता है। बसावट में ख़लल पैदा होता है तो राज्य कमज़ोर पड़ता है और जब राज्य कमज़ोर पड़ता है तो इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए और अधिक ख़र्च की ज़रूरत पड़ती है। ख़र्चों में और वृद्धि होती है। फिर टैक्सों में और वृद्धि करनी पड़ती है और यह नकारात्मक सिलसिला जारी रहता है। यों आख़िरकार राज्य पतन का शिकार हो जाता है।
अत: जब ख़र्चे आमदनी से बढ़ जाएँ, आमदनी कम पड़ने लगे और समाज के ग़रीब वर्ग तबाह होने लगें, जब समाज के दौलतमंद वर्ग अपनी आमदनी अय्याशियों में ख़र्च करने लगें तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपने ख़र्चे कम करने पड़ते हैं। ख़र्चे कम करने में फ़ौज के ख़र्चे भी कम करने पड़ते हैं। फ़ौज के ख़र्चे कम होते हैं तो फ़ौज कमज़ोर होती है, फ़ौज की कमज़ोरी राज्य की कमज़ोरी का कारण बनती है। इसलिए इब्ने-ख़लदून यह कहना चाहता है और तमाम चिन्तकों ने यह बात कही है कि फ़ुज़ूलख़र्ची और आराम-तलबी से हर हाल में बचना चाहिए। इससे शासकों और अधिकारियों की नैतिक स्थिति ख़राब होती है। नैतिक स्थिति ख़राब होने के नतीजे में पॉलिसियाँ ख़राब होती हैं। पॉलिसियाँ ख़राब होने के नतीजे में राज्य पतन का शिकार होता है।
यह बात बहुत-से चिन्तकों ने लिखी है। अल्लामा इक़बाल ने अपने विशिष्ट शायराना अन्दाज़ में कहा है कि तक़दीरे-उमम यह है कि बड़ी-बड़ी हुकूमतों का आरम्भ तो अत्यन्त जुरअत और बहादुरी और तलवारों से होता है, लेकिन जब राज्य क़ायम हो जाए और तलवारों की फ़ौरी ज़रूरत न रहे तो सुबह से लेकर रात तक ऐशो-आराम में जब क़ौम पड़ जाती है, जब राज्य आराम-तलबी और अय्याशियों का शिकार होता है तो गम्भीर मामलों से ध्यान हट जाता है। गम्भीर मामलों से ध्यान हटने की वजह से राज्य में ख़राबियाँ आने लगती हैं।
यही बात ज़रा विभिन्न अन्दाज़ में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है। उन्होंने तफ़सील से बताया है कि राज्य के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए किस ढंग से काम करने की ज़रूरत है। और कौन-कौन से मामलात हैं जिनके नतीजे में राज्य कमज़ोर होता है।
इस्लामी राज्य शुरू ही से दूसरे राज्यों से सम्बन्ध रखता चला आया है। यह सम्बन्ध युद्ध और हथियार के द्वारा भी हुए हैं। शान्ति और समझौतों के द्वारा भी हुए हैं। निष्पक्षता के सम्बन्ध भी हुए हैं। पहले दिन से ही इस्लामी राज्य और दूसरे राज्यों के बीच हर प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध क़ायम रहे हैं। राज्य बनने से पहले ही से मुसलमानों के सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क़ायम थे। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अभी मक्का मुकर्रमा ही में थे कि उन्होंने शासकों को पत्र लिखे। नज्जाशी को पत्र लिखा था कि मेरे कुछ साथी तुम्हारे पास पनाह लेने के लिए आ रहे हैं। उनको पनाह दो और उनकी मदद करो। यह गोया पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क था जो उभरती हुई उम्मते-मुस्लिमा का दूसरे महाद्वीप के एक राज्य के साथ हुआ। पहली शताब्दी ख़त्म होते-होते इस राज्य के सम्बन्ध दुनिया के तमाम बड़े-बड़े राज्यों से क़ायम हो गए। इन सम्बन्धों को संगठित करने के लिए ‘सियर’ के नाम से एक क़ानून पहले से मौजूद था। इस क़ानून को दूसरी और तीसरी शताब्दी हिजरी के आरम्भ में फ़ुक़हा ने विस्तृत रूप से संकलित कर दिया था। दूसरी शताब्दी हिजरी में इमाम यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद-बिन-हसन शैबानी, इमाम शाफ़िई और दूसरे इमामों ने कम-से-कम एक दर्जन किताबें इस क़ानून पर लिखी थीं। यह क़ानून इस्लामी क़ानून का इसी तरह हिस्सा था जैसे क़ानून के शेष विभाग। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का यह क़ानून पहले दिन से पालन योग्य आदेशों का एक संग्रह था। इन्हीं आदेशों के नतीजे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संगठित हो रहे थे और विभिन्न राज्यों से मामलात तय किए जा रहे थे।
यह राज्य जिसके आदेश फ़ुक़हा ने बयान किए, जिसके वैचारिक आधारों को इस्लामी चिन्तकों ने बयान किया, जिसकी बौद्धिक धारणाओं से इस्लाम ने बहस की, जिसकी आध्यात्मिक माँगों पर सूफ़ियों ने चर्चा की, किसी-न-किसी शक्ल में बारह सौ साल तक जारी रहा। इस राज्य की व्यवस्था में निस्सन्देह बहुत-सी कमज़ोरियाँ आईं, अच्छे शासक भी आए, बुरे शासक भी आए, लेकिन मुसलमानों ने कभी भी इस आइडियल को नज़रअन्दाज़ नहीं किया, जिस आइडियल के आधार पर यह राज्य क़ायम हुआ था, अट्ठारहवीं शताब्दी ईसवी में जब मुस्लिम जगत् पश्चिमी उपनिवेशवाद का निशाना बना और मुस्लिम जगत् के अधिकांश देश पश्चिमी शक्तियों के ग़ुलाम हो गए तो हर जगह इस राज्य के एक-बार फिर उत्थान की आवाज़ें उठीं। इस्लाम के लिए संघर्ष करनेवाले आगे बढ़े, उन्होंने इस राज्य के पुनरुत्थान के लिए जानों की क़ुर्बानियाँ दीं, विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने इस राज्य की नई माँगों को बयान किया।
इस अभिलाषा का अत्यन्त प्रबल आभास अनेक देशों में हुआ। उपमहाद्वीप भारत-पाक में भी इस इच्छा और भावना का इज़हार अत्यन्त गहरे चिन्तन के साथ हुआ। यह इज़हार अल्लामा इक़बाल के लेखों में बहुत नुमायाँ है और दूसरे चिन्तकों के लेखकों में भी बहुत अधिक नज़र आता है। जनसाधारण की भावना के रूप में, आन्दोलनों के रूप में, ग़रज़ हर स्थिति में इस भावना का इज़हार हर दौर में हुआ। ख़िलाफ़त आन्दोलन के रूप में यही भावना एक नए अन्दाज़ से सामने आई। इसी तरह पाकिस्तान आन्दोलन के रूप में जो एक इस्लामी राज्य की स्थापना एक सामूहिक कोशिश थी, यही भावना कार्यरत थी। पाकिस्तान आन्दोलन दरअस्ल उन पश्चिमी धारणाओं के इनकार पर बना था जो आधुनिक काल में प्रचलित थीं और आधुनिक धर्म विरोधी और राजनैतिक धारणाओं पर आधारित थीं। पाकिस्तान की परेशानी और मुश्किलों एक बड़ा कारण भी येही है कि जो लोग पाकिस्तान पर हावी हुए वे उस आन्दोलन की रूह से बिल्कुल अनजान रहे हैं। इस वर्ग ने आधुनिक अधर्मी पश्चिमी धारणाओं को पाकिस्तान में जारी करना चाहा। पाकिस्तान वासियों के मनोविज्ञान और स्वभाव ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए कश्मकश पैदा हुई। इस कश्मकश का इज़हार विभिन्न रूप में होता रहा है। आज भी समय-समय पर पाकिस्तान के विभिन्न इलाक़ों में जो आवाज़ें उठती हैं जिसपर हमारा शासक वर्ग नाराज़ होता है, वह इसी इच्छा की अभिव्यक्ति है जिसकी सख़्त और प्रबल अभिव्यक्ति इस्लामीआन्दोलन में हुई और जिसकी पूर्ति के लिए यह देश अस्तित्व में आया था। इन कोशिशों या प्रयासों का जवाब शक्ति का प्रयोग नहीं है। इन कोशिशों का जवाब इस्लामीआन्दोलन की अस्ल स्प्रिट की तरफ़ पलटना है। दरअस्ल प्रोफ़ेसर आर्बरी ने आज से लगभग पचपन साल पहले लिखा था कि पाकिस्तान के लोगों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज क़ुबूल किया है। और इतिहास बताएगा कि यह बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लोग उठा सकते हैं और उसको निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते।
मुहम्मद अली जिनाह के शब्दों में पाकिस्तान एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर अस्तित्व में आया था जहाँ दुनिया को यह दिखाना अभीष्ट था कि इस्लाम के सिद्धान्त आज भी उसी तरह प्रभावशाली और काम कर रहे हैं जिस तरह आज से चौदह सौ साल पहले काम करते थे। लेकिन पाकिस्तान के अब तक के तमाम शशक पाकिस्तान-वासियों की अभिलाषा को वास्तविकता का रूप प्रदान करने में नाकाम हो गए । तमाम परेशानियों और मुश्किलों जिसमें आज पाकिस्तान के लोग मुब्तला नज़र आते हैं। इन परेशानियों की बड़ी ज़िम्मेदारी उस अयोग्य, कम समझ और निष्ठा रहित नेतृत्व पर लागू होती है जो पाकिस्तान-वासियों पर प्रभावी हो गया। यहाँ नेतृत्व से मुराद मात्र शासक नहीं हैं, बल्कि वे तमाम लोग मुराद हैं जो किसी-न-किसी अन्दाज़ में इस क़ौम के नेतृत्व के दावेदार रहे हैं, जो धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या वैचारिक मामलों में क़ौम की राहनुमाई का लबादा ओढ़े हुए हैं।
Recent posts
-

इस्लामी शरीअत का भविष्य और मुस्लिम समाज का सभ्यता मूलक लक्ष्य (शरीअत : लेक्चर# 12)
02 December 2025 -
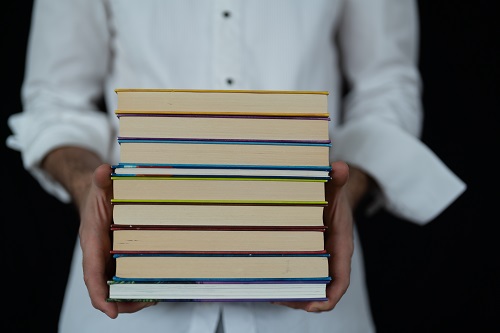
इस्लामी शरीअत आधुनिक काल में (शरीअत : लेक्चर# 11)
25 November 2025 -

इल्मे-कलाम अक़ीदे और ईमानियात की ज्ञानपरक व्याख्या एक परिचय (शरीअत : लेक्चर# 10)
21 November 2025 -

अक़ीदा और ईमानियात - शरई व्यवस्था का पहला आधार (शरीअत : लेक्चर# 9)
17 November 2025 -

तज़किया और एहसान (शरीअत : लेक्चर# 8)
12 November 2025 -

इस्लाम में परिवार की संस्था और उसका महत्त्व (शरीअत : लेक्चर# 6)
24 October 2025