
सूद का हराम होना और इसका मूल कारण (लेक्चर-7)
-
अर्थशास्त्र
- at 03 February 2026
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
आज की चर्चा का शीर्षक है—‘रिबा (सूद) का हराम होना और इसका मूल कारण”। पवित्र क़ुरआन, हदीस और फ़िक़्हे-इस्लामी (इस्लामी धर्मशास्त्रों) का हर विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि शरीअत ने ‘रिबा’ को स्पष्ट रूप से हराम क़रार दिया है और न केवल हराम क़रार दिया है, बल्कि उसके हराम होने और उसकी बुराई को इतने स्पष्ट, दो-टूक और साफ़ शब्दों में बयान किया है कि इससे ज़्यादा स्पष्टता और शिद्दत कम मामलों में नज़र आती है। ‘रिबा’ वह एकमात्र अपराध है जिसकी सज़ा के तौर पर अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ से ब्याज खानेवालों और ‘रिबा’ का कारोबार करनेवालों के ख़िलाफ़ एलाने-जंग किया है। अल्लाह तआला ने या उसके रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने ब्याजख़ोरी के अलावा किसी और अपराध के करनेवालों के ख़िलाफ़ एलाने-जंग नहीं किया यहाँ तक कि किसी इंसान की हत्या या दूसरी नैतिक बुराइयाँ जो शरीअत की नज़र में अत्यन्त मकरूह (अप्रिय) और नापसंदीदा हैं, उनका इर्तिकाब करनेवालों के ख़िलाफ़ भी एलाने-जंग नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि शरीअत द्वारा हराम ठहराई हुई चीज़ों में ‘रिबा’ के हराम होने का दर्जा क्या है और ‘रिबा’ और मामलों से बचने का शरीअत में क्या महत्व है।
उर्दू भाषा में ‘रिबा’ का अनुवाद सूद (ब्याज) के शब्द से किया जाता है। सच तो यह है कि ‘रिबा’ और ब्याज में शब्दकोशीय दृष्टि से कोई विशेष अनुकूलता नहीं है। अरबी भाषा में ‘रिबा’ के अर्थ हैं ज़्यादती या बढ़ोतरी। जब किसी चीज़ में कोई ज़्यादती हो, बढ़ोतरी हो या वह पहले से बढ़ जाए तो उसके लिए अरबी भाषा में ‘रिबा’ का शब्द प्रयुक्त होता है। पवित्र क़ुरआन में ‘रिबा’ का शब्द अपने शाब्दिक अर्थ में कई जगह प्रयुक्त हुआ है। एक जगह कहा गया है, ‘व युरबिस-स-दक़ाति’ अर्थात् “अल्लाह तआला सदक़ात को बढ़ाता है।” (क़ुरआन, 2:276)। अगर इंसान सदक़ा करे तो अल्लाह तआला उसके अज्रो-सवाब (प्रतिदान) में लगातार वृद्धि करता रहता है। पवित्र क़ुरआन में ‘रबवह’ का शब्द भी आया है जो किसी ऊँचे भूभाग के लिए प्रयुक्त होता है। ‘वावयना हुमा इला रबविन ज़ाति क़रारिन व मईन’ अर्थात् “हमने हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) और उनकी माँ को एक ऐसी बुलंद ज़मीन पर ठिकाना प्रदान किया जहाँ ठंडा पानी भी था और उनके लिए रहने की जगह भी थी।” (क़ुरआन, 26:50) एक और जगह पवित्र क़ुरआन में आया है ‘अहत-ज़-रत व-रबत’ अर्थात् “जब खेती पूरी तरह से खिलखिलाने लगती है और बढ़ जाती है।” (क़ुरआन, 41:39) इस दृश्य को बयान करने के लिए पवित्र क़ुरआन ने ये दो शब्द प्रयुक्त किए हैं। एक और जगह है ‘फ़-आ ख़-ज़हुम अख़ज़तर-राबिया’ अर्थात् “अल्लाह तआला ने उनकी पकड़ की इस तरह की कि इससे बढ़कर पकड़ नहीं हो सकती।” (क़ुरआन, 69:10) ‘राबिया’ अरबी भाषा में ऊँचे भूभाग को भी कहा जाता है।
‘रबवह’ और ‘राबिया’ का अर्थ मानो एक ही है। इन शाब्दिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘रिबा’ के शाब्दिक अर्थ में बढ़ोतरी और ज़्यादती का मतलब शामिल है। एक हदीस में भी एक सहाबी ‘रिबा’ का शब्द ज़्यादती के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम दोनों में एक जगह रिवायत आई है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक मौक़े पर खाने में बरकत की दुआ की। सहाबा किराम जो यह रिवायत करते हैं वे यह बयान करते हैं कि इस दुआ की बरकत इतनी ग़ैर-मामूली थी कि जब हम कोई निवाला उठाते थे तो लगता था कि वह बढ़ रहा है। नीचे से इस निवाले में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ भी ‘रिबा’ का शब्द बढ़ोतरी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
‘रिबा’ के इन शाब्दिक अर्थों के साथ-साथ अरबी भाषा में ‘रिबा’ का शब्द एक आर्थिक शब्दावली के तौर पर भी अज्ञानकाल ही से प्रयुक्त होता था। मामलात (व्यवहार) और ख़रीदने-बेचने के आदेशों से सम्बन्धित हदीसों में ‘रिबा’ का शब्द इन्ही पारिभाषिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।
ये शब्द इसी पारिभाषिक अर्थ में पवित्र क़ुरआन और हदीसों में भी कई बार प्रयुक्त हुआ है। सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) और ताबिईन के कथनों में ‘रिबा’ का शब्द पारिभाषिक अर्थ में बार-बार आया है।
‘रिबा’ की परिभाषा फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने क्या की है, इसकी तरफ़ भी मैं आता हूँ, लेकिन यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम से पहले सूदी (ब्याज आधारित) कारोबार पूरे अरब में प्रचलित था। अरब के व्यापारी ‘रिबा’ की हक़ीक़त पूरे तौर पर जानते थे। उनमें से किसी के ज़ेहन में यह उलझन नहीं थी कि ‘रिबा’ किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते। इसलिए जब पवित्र क़ुरआन ने ‘रिबा’ के हराम होने का आदेश अवतरित किया तो पवित्र क़ुरआन के हर पाठक और श्रोता ने यह समझ लिया कि किस चीज़ को हराम क़रार दिया जा रहा है। पवित्र क़ुरआन के आरम्भिक श्रोताओं में से किसी के ज़ेहन में बिलकुल यह उलझन नहीं थी कि ‘रिबा’ से क्या मुराद है, न उनको इसकी ज़रूरत थी कि उनके लिए ‘रिबा’ की कोई कलात्मक ढंग की परिभाषा बयान की जाए। फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने ‘रिबा’ की जो परिभाषाएँ की हैं वे दर्सी (पाठ्य सम्बन्धी) ज़रूरतों के लिए की हैं। ये परिभाषाएँ इसलिए नहीं कीं कि अगर वे ‘रिबा’ की यह परिभाषा नहीं करते तो ‘रिबा’ का हराम होना स्पष्ट न होता। ‘रिबा’ की हक़ीक़त तो पहले से स्पष्ट थी और न केवल ‘रिबा’ की हक़ीक़त स्पष्ट थी, बल्कि पवित्र क़ुरआन और हदीसों और शरीअत के तमाम पारिभाषिक शब्द अच्छी तरह से स्पष्ट थे और निश्चित अर्थ एवं भावार्थ रखते थे। फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने इन सब पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ दर्सी (पाठ्य सम्बन्धी) ज़रूरतों के लिए शोधार्थ एवं लेखनार्थ करना उचित समझा। इन परिभाषाओं से यह समझना कि ‘रिबा’ या कोई और शब्दावली पहले से स्पष्ट या निर्धारित नहीं थी, फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) के निर्धारित करने से निर्धारित हुई, यह अत्यन्त ग़लत-फ़हमी और नासमझी की बात है।
उदाहरण के रूप में पवित्र क़ुरआन में नमाज़ की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन ‘इक़ामते-सलात’ (नमाज़ क़ायम करने) का आदेश बार-बार दिया गया है। लेकिन ‘सलात’ की इस तरह की दर्सी (पाठ्य) या कलात्मक ढंग की परिभाषा पवित्र क़ुरआन या हदीस में कहीं मौजूद नहीं है जो फ़िक़्ह (धर्मशास्त्र) की किताबों में मिलती है। इस तरह पवित्र क़ुरआन में ज़कात का आदेश है, हज का आदेश है, जिहाद का आदेश है। उनमें से किसी शब्दावली की इस ढंग की परिभाषा नहीं की गई जिस ढंग की परिभाषा फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) की शैली के अनुसार की जाती है। पवित्र क़ुरआन की शैली और अंदाज़ यह है कि जब वह किसी चीज़ का आदेश देता है या किसी चीज़ को हराम (निषिद्ध) क़रार देता है तो उसके लिए आम तौर से वह शब्दावली प्रयुक्त करता है जो पहले से अरब में प्रचलित हो। जैसे हज की शब्दावली प्रचलित थी। पवित्र क़ुरआन ने हज की शब्दावली प्रयुक्त की। उमरे की शब्दावली प्रयुक्त की। इन पारिभाषिक शब्दों से अरब के लोग हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) के ज़माने से परिचित थे।
जहाँ पवित्र क़ुरआन कोई नई शब्दावली प्रयुक्त करता है, वहाँ अपनी विशेष शैली में उसकी व्याख्या भी करता है। उदाहरणार्थ ज़कात की शब्दावली नई है। सलात की शब्दावली अरबी भाषा के इस विशेष अर्थ में नई है। इन नई क़ुरआनी शब्दावलियों की व्याख्या का तरीक़ा पवित्र क़ुरआन में यह नहीं है कि पहले इस शब्दावली की कलात्मक ढंग में परिभाषा बयान करे। जिस तरह क़ानूनी शब्दावली की कलात्मक परिभाषाएँ क़ानून के शुरू में दी जाती हैं, उस तरह परिभाषाएँ दी जाएँ। यह पवित्र क़ुरआन का ढंग नहीं है। पवित्र क़ुरआन एक विशेष शब्दावली प्रयुक्त करता है। उसके विभिन्न पहलुओं की बार-बार विभिन्न तरीक़ों से निशानदेही करता जाता है। फिर जगह-जगह पवित्र क़ुरआन में इसके बारे में आदेश दिए जाते हैं। इन सब आदेशों पर लगातार विचार करने से और इनको एक-दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ने से इस शब्दावली का पूरा अर्थ और वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। फिर हदीसों के ज़रिये, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत के ज़रिये इस शब्दावली की और अधिक पड़ताल, अधिक व्याख्या और अधिक निश्चयन हो जाता है। जहाँ-जहाँ अस्पष्टता महसूस हो, या किसी ग़लत-फ़हमी की सम्भावना हो तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) इस ग़लत-फ़हमी को दूर कर देते हैं। इस तरह पवित्र क़ुरआन की विभिन्न आयतों और हदीसों में बयान किए गए विवरण को सामने रखने से उन तमाम पारिभाषिक शब्दों और आदेशों की व्याख्या पूर्ण रूप से हो जाती है जो पवित्र क़ुरआन में बयान हुए हैं।
‘रिबा’ की जो कलात्मक परिभाषा फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने की है उसकी ओर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले एक बात ज़ेहन में रखनी चाहिए, वह यह कि ‘रिबा’ की बड़ी-बड़ी क़िस्में दो हैं। ‘रिबा’ की एक क़िस्म तो वह है जिसको ‘रिबाउन-सैयेआ’ कहा जाता है। यानी उधार पर दिया जानेवाला ब्याज। इसी को ‘रिबाउल-जाहिलिया’ भी कहा जाता है। यानी वह ‘रिबा’ जो अज्ञानकाल के दौर में प्रचलित था और अज्ञानकाल के लोग जिस ‘रिबा’ को जानते थे। उसी को ‘रिबाउल-क़ुरआन’ भी कहा जाता है कि पवित्र क़ुरआन ने स्पष्ट रूप से जिस ‘रिबा’ को हराम कहा है वह यही है। ‘रिबाउन-सैयेआ’, ‘रिबाउल-जाहिलिया’ ‘रिबाउल-क़ुरआन’ से मुराद यह है कि किसी व्यक्ति के ज़िम्मे कोई रक़म क़र्ज़ हो जिसको अदा करने के लिए कोई अवधि निर्धारित हो। इस भुगतान की अवधि को बढ़ा दिया जाए और इस बढ़ोतरी के मुक़ाबले में कोई बढ़ी हुई रक़म वुसूल की जाए, इसको ‘रिबाउन-सैयेआ’ कहा जाता था। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति को एक हज़ार रुपये अदा करने थे, एक महीने बाद अदा करने थे, वह एक महीने बाद अदा नहीं कर सका। अब वह चाहता है कि उसको एक महीने की और मोहलत मिल जाए। अज्ञानकाल में इस अधिक मोहलत की क़ीमत वुसूल की जाती थी। गोया वक़्त की क़ीमत वुसूल की जाती थी। इस वक़्त की क़ीमत वुसूल करने ही का नाम ‘रिबाउन-सैयेआ’ या ‘रिबाउल-जाहिलिया’ था। या किसी व्यक्ति ने किसी से क़र्ज़ लिया और क़र्ज़ की अवधि उदाहरणार्थ एक साल है, छः महीने है, चार महीने है। इस अवधि के मुक़ाबले में मूल धन से अधिक जो रक़म ली जाती थी वह भी ‘रिबा’ कहलाती थी। गोया मूल धन पर वृद्धि हो या बाद में क़र्ज़ अस्ल और ब्याज दोनों में मिलाकर फिर वृद्धि हो, दोनों को ‘रिबा’ कहा जाता था। यह तो ‘रिबा’ की सबसे बड़ी क़िस्म थी और वास्तविक अर्थ में ‘रिबा’ यही है। ‘रिबा’ की एक दूसरी क़िस्म वह भी है जिसको ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ कहा गया है, या ‘रिबाउल-हदीस’ भी कहा गया है, या ‘रिबाउल-बुयूअ’ भी कहा गया। ‘रिबा’ की यह क़िस्म हदीसों के ज़रिये हराम क़रार दी गई है और यह अस्ल में हल्के दर्जे का ‘रिबा’ गुप्त प्रकार का ‘रिबा’ है जो बड़े और अस्ल ‘रिबा’ का रास्ता रोकने के लिए हराम क़रार दिया गया है। शरीअत का एक स्वभाव जो जगह-जगह नज़र आता है वह यह भी है कि शरीअत जब किसी चीज़ को हराम क़रार देती है तो उन तमाम रास्तों को भी हराम क़रार दे देती है जो उस बड़े हराम काम को करने का ज़रिया बन सकें। इसकी अनगिनत मिसालें शरीअत के आदेशों में मिलती हैं।
चूँकि ‘रिबा’ का रास्ता खोलनेवाले बहुत-से द्वार हैं। बहुत-से रास्ते ऐसे हैं कि जो इंसानों ने ईजाद किए। बज़ाहिर शुरू में उनमें कोई बुराई मालूम नहीं होती, लेकिन अगर इस रास्ते पर इंसान चल पड़े तो धीरे-धीरे उसकी बुराई स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है और आख़िरकार वह ‘रिबा’ के जुर्म तक पहुँचा देता है। इस तरह के तमाम रास्तों को शरीअत ने बंद किया है। मैं पहले बता चुका हूँ कि शरीअत में जिन-जिन प्रकार के कारोबारों की मनाही की गई है, छप्पन प्रकार के कारोबार हैं और ये सब कारोबार वे थे जो आख़िरकार ‘रिबा’ पर पहुँचा देते थे या ‘क़िमार’ (जुआ) और ‘ग़रर’ (धोखाधड़ी) पर निर्भर होते थे। इन्ही रास्तों की एक बड़ी क़िस्म ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ भी है।
‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ अस्ल में बार्टर सेल में होता था, जब क्रय-विक्रय वस्तु के बदले वस्तु के रूप में होता था। अरब में आम तौर से और मदीना मुनव्वरा में विशेष रूप से बार्टर सेल का बहुत प्रचलन था। मदीना मुनव्वरा एक कृषि आबादी थी। थोड़े-बहुत स्थानीय उद्योग भी थे। इसलिए कृषि उत्पादन में हिस्सा लेनेवाले लोग अपनी पैदावार को बार्टर के द्वारा बेचा करते थे। और चूँकि मदीना मुनव्वरा में आम तौर पर लोगों की ख़ुराक जौ होती थी या खजूर होती थी, इसलिए जौ और ख़जूरों की ज़रूरत हर समय व्यक्ति को रहती थी। जो लोग ज़मीनों के मालिक थे, जिनमें बहुत बड़ी संख्या यहूदियों की थी, वे लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे। और इस दावे की बुनियाद पर कि फ़ुलाँ खजूर घटिया है, और फ़ुलाँ बढ़िया है, और फ़ुलाँ की मालियत ज़्यादा है, फ़ुलाँ की मालियत कम है, इन बुनियादों पर या इन बहानों से चीज़ों में कमी-बेशी किया करते थे। जो दरअस्ल वक़्त की क़ीमत होती थी। उदाहरणार्थ आज एक व्यक्ति को ख़जूरों की ज़रूरत है, उसके घर में खजूरें ख़त्म हो गईं या उदाहरणार्थ जौ की ज़रूरत है, गेहूँ की ज़रूरत है। उसको आवश्यकतानुसार जौ या गेहूँ दे दिया और जब फ़स्ल कटने पर उसके भुगतान का समय आया तो दावा किया कि मैंने जो तुम्हें गेहूँ दिया था वह बहुत बढ़िया था और जो तुम मुझे दे रहे हो वह घटिया है। लिहाज़ा तुम मुझे उसका दो गुना अदा करो। या जो वक़्त गुज़रा है, छः महीने, उसके मुक़ाबले में अगर तुमने मुझसे डेढ़ मन गेहूँ लिया था तो आप दो गुना अदा करो। यह सब बहाने दरअस्ल ब्याजख़ोरी का रास्ता खोलने के बहाने थे। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसकी मनाही की और उन चीज़ों के लेन-देन में कमी-बेशी को नाजायज़ क़रार दिया।
कमी-बेशी के लिए अरबी भाषा में ‘फ़ज़्ल ‘और ‘तफ़ाज़ुल’ की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसलिए इसको ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ के नाम से याद किया जाने लगा। ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ के निषेध का आधार वे हदीसें हैं जिनको कई सहाबा किराम ने बयान किया है। और लगभग तमाम बड़े मुहद्दिसीन ने इन हदीसों को नक़्ल किया है। इन हदीसों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “सोने का क्रय-विक्रय सोने के मुक़ाबले में, चाँदी का क्रय-विक्रय चाँदी के मुक़ाबले में, गेहूँ का क्रय-विक्रय गेहूँ के मुक़ाबले में, जौ का क्रय-विक्रय जौ के मुक़ाबले में, खजूर का क्रय-विक्रय खजूर के मुक़ाबले में अगर हो तो हाथ-के-हाथ हो और कमी-बेशी के साथ न हो। अगर कमी-बेशी होगी या हाथ-के-हाथ नहीं होगा तो यह ‘रिबा’ होगा।” इन हदीसों की बुनियाद पर फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने सर्वसहमति से ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ को हराम क़रार दिया है। और उसी तरह हराम क़रार दिया है जिस तरह ‘रिबाउन-सैयेआ’ हराम है। इन दोनों परिभाषाओं को सामने रखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तविक ‘रिबा’ तो ‘रिबाउन-सैयेआ’ ही है। और ‘रिबाउल-फ़ज़्ल’ का निषिद्ध होना उसका रास्ता रोकने के लिए है। फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने कोशिश यह की है कि ‘रिबा’ की कोई ऐसी परिभाषा की जाए कि इसमें ‘रिबा’ की दोनों किस़्में स्पष्ट हो सकें, ‘रिबाउद्दैन’ या ‘रिबाउल-जाहिलिया’ या ‘रिबाउन-सैयेआ’ भी इसमें शामिल हो जाएँ। और ‘रिबाउल-बुयूअ’ भी इसकी परिभाषा में आ सके। ‘रिबाउल-बुयूअ’ के बारे में मैं कह चुका हूँ कि यह उस ज़माने के बार्टर सेल में होता था। इसलिए आज इसका अधिक महत्व नहीं रहा। आज बार्टर सेल का ज़माना ख़त्म हो गया। इसलिए कि आपस में वस्तुओं के तबादले का रिवाज अब नहीं रहा। इसलिए ‘रिबा’ की पुरानी फ़िक़्ही परिभाषाएँ आज ज़्यादा जानी-पहचानी नहीं रहीं। इसलिए कि फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने ‘रिबा’ की दोनों क़िस्मों को एक ही परिभाषा के ज़रिये बयान करने की कोशिश की थी।
चूँकि यह परिभाषाएँ जो पाठ्य सम्बन्धी और कलात्मक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं, इसलिए इनका मूल उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों को इस एक व्यापक परिभाषा के द्वारा ‘रिबा’ की दोनों क़िस्मों का हराम होना स्पष्ट रूप से समझा दिया जाए। आजकल कुछ आधुनिकतावादी ‘रिबाउल-बुयूअ’ का उल्लेख करके उलझाने का प्रायस करते हैं। ‘रिबाउल-बुयूअ’ जिसको कहा जाता है, आज वह बहुत सीमित पैमाने पर रह गया है। ‘रिबा’ की सबसे बड़ी क़िस्म अतीत में भी ‘रिबाउन-सैयेआ’ थी और आज भी ‘रिबाउन-सैयेआ’ ही है। इसलिए ‘रिबा’ की कोई ऐसी परिभाषा जिसमें ‘रिबाउन-सैयेआ’ शामिल न हो या जिसके द्वारा किसी शाब्दिक बाज़ीगरी के आधार पर ‘रिबाउन-सैयेआ’ को निकाला जा सके, एक नकारात्मक और कुत्सित प्रयास है। ऐसा करना शरीअत के मंशा के ख़िलाफ़ है और शरीअत के उद्देश्य को नाकाम बनाने के समान है।
मशहूर हनफ़ी फ़क़ीह इमाम ज़ैलई ने ‘रिबा’ की परिभाषा की है कि “माल के मुक़ाबले में जब माल वुसूल किया जाए और एक तरफ़ से उसमें बिना किसी बढ़े हुए बदले के वृद्धि हो, उसको ‘रिबा’ कहा जाता है।” उदाहरणार्थ आपने एक लाख रुपये चुकाकर कोई चीज़ ख़रीद ली, पुरानी गाड़ी ख़रीद ली, कोई पुरानी मशीनरी आपने ख़रीद ली।
अब एक तरफ़ जो माल है वह मशीनरी है जिसकी मालियत आप दोनों ने बाज़ार के भाव के अनुसार एक लाख रुपये तय की है। दूसरी तरफ़ का माल एक लाख रुपये नक़द है। अब जब एक व्यक्ति इस एक लाख रुपये का एक महीने बाद भुगतान की मोहलत देते हुए इस एक महीने के मुक़ाबले में एक लाख रुपये से ज़्यादा बढ़ी हुई रक़म वुसूल करेगा तो यह बढ़ी हुई रक़म ‘रिबा’ कहलाएगी। फ़िक़्ह में बयान की गई ‘रिबा’ की परिभाषा के अनुसार यह बढ़ोतरी ‘रिबा’ हो जाएगी। अगर एक मन गेहूँ के मुक़ाबले में डेढ़ मन गेहूँ वुसूल करेगा तो यह भी आधे मन की ज़्यादती की वजह से ‘रिबा’ की इस परिभाषा में आएगा। ‘रिबा’ की वे तमाम परिभाषाएँ जो फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने की हैं वे इसी से मिलती-जुलती हैं। शब्दों में थोड़ा-बहुत अन्तर कहीं-कहीं पाया जाता है। लेकिन भावार्थ तमाम परिभाषाओं का यही है। यहाँ जिस चीज़ को ज़्यादती या ‘तफ़ाज़ुल’ कहा गया है, उसमें वास्तविक ‘तफ़ाज़ुल’ और ज़्यादती भी शामिल है और हुक्मी और एतिबारी ‘तफ़ाज़ुल’ और ज़्यादती भी शामिल है। हुक्मी ‘तफ़ाज़ुल’ और ज़्यादती शरीअत ने मोहलत को क़रार दिया है। अगर दो यकसाँ चीज़ों की, सोने की सोने के साथ, चाँदी की चाँदी के साथ, गेहूँ की गेहूँ के साथ, ख़रीद-बिक्री, लेन-देन होगा या क्रय-विक्रय होगा, तो इसमें अगर हाथ-के-हाथ न हो तो यह अवधि की जो छूट है यह भी एतिबारी लिहाज़ से या हुक्मी दृष्टि से बढ़ोतरी के समान है। इसलिए शरीअत ने इसकी इजाज़त नहीं दी।
एक और फ़क़ीह ने ‘रिबा’ की परिभाषा करते हुए कहा है कि “किसी वस्तु का क्रय-विक्रय उसी वस्तु के साथ, ज़्यादती के साथ या भुगतान में देर के साथ किया जाए तो यह ‘रिबा’ है।” कुछ और फुक़हा ने कुछ हदीसों को सामने रखकर परिभाषा की है कि ‘रिबा’ से मुराद उस माल का लाभ है जिसके नुक़्सान या जुर्माने का इंसान ज़िम्मेदार न हो। यह प्रत्यक्ष रूप से दो हदीसों से लिया गया है। एक तो मशहूर हदीस है जो तमाम फुक़हा के यहाँ बुनियादी क़ानूनी उसूल की हैसियत रखती है, वह है “जिस चीज़ का इंसान फ़ायदा उठाना चाहता है वह उसी चीज़ का उठा सकता है जिसके नुक़्सान का भी वह ज़िम्मेदार हो।” इसी तरह जिस चीज़ के नुक़्सान का वह ज़िम्मेदार है उसका फ़ायदा उठाने का भी हक़ रखता है। यह नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए तो मौजूद हों और उसका घाटा या नुक़्सान उठाने के लिए आमादा न हों। या किसी चीज़ का नुक़्सान तो आपपर डाल दिया जाए और उसका फ़ायदा उठाने की आपको इजाज़त न हो। यह शरीअत के अनुसार न्याय एवं समानता की परिकल्पना के ख़िलाफ़ है। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्पष्ट रूप से उस सौदे की मनाही की है जिसके द्वारा ऐसी चीज़ का लाभ वुसूल किया जाए जिसका घाटा या जुर्माना इंसान के ज़िम्मे न हो। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इस बात से मना किया है कि “जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी, या जुर्माना या घाटा किसी इंसान के ज़िम्मे न हो वह उसका लाभ नहीं उठा सकता।”
यह है ‘रिबा’ की हक़ीक़त जो अरब में मालूम और निर्धारित थी। मक्का के इस्लाम विरोधी भी ‘रिबा’ की इस हक़ीक़त को जानते थे और उसको नाजायज़ और नापाक समझते थे। यह समझना कि अरब में ‘रिबा’ को जायज़ और हलाल माना जाता था और इस्लाम ने पहली बार उसको हराम क़रार दिया है, दुरुस्त नहीं है। ‘रिबा’ इस्लाम से पहले भी हराम था। अरब के लोग भी इसको हराम और बुरा ही समझते थे और इस्लाम से पहले की शरीअतों में भी ‘रिबा’ हराम था। आपको याद होगा कि जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की नौजवानी के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में सैलाब आया और बैतुल्लाह (काबा) की इमारत को नुक़्सान पहुँचा, उस समय क़ुरैश के इस्लाम-विरोधियों ने यह तय किया था कि वे बैतुल्लाह का नए सिरे से निर्माण करेंगे। इस नवनिर्माण के काम में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी एक नौजवान की हैसियत से शरीक थे। इस अभियान में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने चचाओं के साथ शरीक हुए थे। इब्ने-हिशाम जो इस्लाम के मुख्य दौर के सबसे बड़े सीरत निगार (जीवनी लेखक) हैं लिखते हैं कि जब क़ुरैश यह फ़ैसला कर रहे थे तो उन्होंने एक-दूसरे से कहा कि देखो काबे के तामीर में कोई नापाक आमदनी प्रयुक्त न हो। केवल पाकीज़ा आमदनी ही इस नेक काम में इस्तेमाल की जाए। चुनाँचे हरामकारी के नतीजे में कमाई जानेवाली कोई रक़म ब्याजख़ोरी के द्वारा आनेवाली आमदनी किसी इंसान पर ज़ुल्म के नतीजे में हासिल होनेवाली रक़म इसमें ख़र्च न की जाए। ये तीन प्रकार की आमदनियाँ उन्होंने हराम और नापाक समझीं, उनको नाजायज़ क़रार दिया। हराम कामों के द्वारा कमाई जानेवाली रक़म, ब्याजख़ोरी के द्वारा होनेवाली आमदनी और किसी इंसान पर ज़ुल्म करके उसकी हथियाई हुई रक़म, इन तीनों को उन्होंने नापाक क़रार दिया और बैतुल्लाह (काबा) के निर्माण में ऐसी रक़म लगाने को बैतुल्लाह के सम्मान के ख़िलाफ़ समझा। केवल मक्का के इस्लाम-विरोधी ही नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले की तमाम शरीअतों में भी ‘रिबा’ की ‘हुर्मत’ (निषिद्ध होने) के आदेश स्पष्ट रूप से हमेशा मौजूद रहे हैं। ख़ुद पवित्र क़ुरआन की गवाही मौजूद है। यहूदियों के अपराधों का जहाँ उल्लेख है वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहूदियों के ब्याजख़ोरी या ‘रिबा’ में लिप्त होने के कारण उन्हें फ़ुलाँ-फ़ुलाँ सज़ाएँ दी गईं, हालाँकि उनको ब्याजख़ोरी से रोका गया था। यह सूद (ब्याज) के हराम होने का स्पष्ट प्रमाण है। ईसाइयों में एक लम्बे समय तक ‘रिबा’ और सूद के हराम होने पर मतैक्य भी रहा है और अधिकतर ईसाई इसपर अमल भी करते रहे हैं। यहूदियों और ईसाइयों के अलावा दूसरे धर्मों में भी ‘रिबा’ का निषिद्ध होना सर्वमान्य मामले की हैसियत रखता रहा है। हिंदुओं में ब्याज के नाम से जो चीज़ मशहूर थी यह वही थी जिसको अरबी भाषा में ‘रिबा’, उर्दू और फ़ारसी में सूद और आजकल अरब दुनिया में फ़ायदा कहा जाने लगा है। मूसा (अलैहि॰) की शरीअत में किताब निर्गमन और किताब व्यवस्थाविवरण में, ईसा (अलैहि॰) की शरीअत में लूक़ा की इंजील में स्पष्ट रूप से ‘रिबा’ की निन्दा के आदेश आज भी मौजूद हैं। अफ़लातून और अरस्तू के लेखों में ‘रिबा’ के बारे में अत्यन्त नकारात्मक बातें मौजूद हैं। पश्चिम के धार्मिक इतिहास के बहुत बड़े सुधारक लूथर के लेखों में ‘रिबा’ के हराम होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। ‘रिबा’ के विषय में एक मूलभूत और महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, न केवल ‘रिबा’ के विषय में, बल्कि यह आदेश शरीअत के तमाम मामलों और लेन-देन से सम्बन्धित हर प्रकार के कारोबार में दिया गया है। “कोई व्यवसाय या लेनदेन हलाल है या हराम यह उसकी सामग्री और विषय वस्तु पर निर्भर करता है, उसके बाह्य रूप या शीर्षक पर नहीं।” चुनाँचे देनेवाला और लेनेवाला कोई भी हो, देनेवाला व्यक्ति हो या अंजमुन हो, संस्था हो या सरकार हो। रज़ामंदी से दे रहा हो या नाराज़ी से। उसका नाम ‘रिबा’ रखा जाए, लाभ रखा जाए, फ़ायदा रखा जाए, Intrest रखा जाए, कुछ भी रखा जाए, लेनेवाले ज़रूरतमंद हों या सम्पन्न हों। लेनेवाले का मक़सद व्यापारिक हो या उपभोगी हो, निजी हो या कारोबारी हो, जहाँ जब और जिस रूप में ‘रिबा’ की हक़ीक़त या गुण पाया जाएगा वह ‘रिबा’ होगा।
यह कहना कि चूँकि अस्ल रक़म पर यह बढ़ोतरी तिजारत के उद्देश्य से ली जा रही है अतः रिबा नहीं है, यह कहना कि देनेवाला फ़क़ीर और ज़रूरतमंद नहीं है इसलिए यह ‘रिबा’ नहीं है। यह कहना कि सूद पर क़र्ज़ लेनेवाला रज़ामंदी से ले रहा है, देनेवाला रज़ामंदी से दे रहा है इसलिए ‘रिबा’ नहीं है। यह कहना कि सूद लेनेवाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि सरकार या कोई संस्था है, इसलिए ‘रिबा’ नहीं है। ये तमाम तर्क कमज़ोर बहाने हैं, और ये तमाम बाहरी चीज़ें असम्बन्धित हैं। जो उसूल है शरीअत का वह यह है कि मामलात में, लेन-देन और व्यापार में अस्ल एतिबार हक़ीक़त और स्वरूप का होता है, शीर्षक और ज़ाहिरी शब्दों का नहीं। अस्ल महत्व शीर्षक को नहीं सामग्री को हासिल होता है। दूसरी बात यह याद रखने की है कि ‘रिबा’ के हराम होने का ताल्लुक़ अल्लाह के अधिकारों से है, मूलरूप से यह अल्लाह का हक़ है। इसलिए यह कहना कि चूँकि दोनों पक्ष राज़ी हैं इसलिए सूदी व्यापार जायज़ होना चाहिए यह दुरुस्त नहीं है। शरीअत के बहुत-से आदेश ऐसे हैं कि जिसमें अस्ल ‘हक़्क़ुल्लाह’ का हक़ है। अल्लाह के हक़ को कोई रद्द नहीं कर सकता, अल्लाह के हक़ को कोई माफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह के हक़ में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कमी-बेशी नहीं कर सकता। इसलिए किसी पक्ष के राज़ी या नाराज़ होने से ‘रिबा’ का हराम होने पर फ़र्क़ नहीं पड़ता। अगर दोनों पक्षों में रज़ामंदी की वजह से ‘रिबा’ का कारोबार जायज़ क़रार पाए तो रज़ामंदी से तो और भी बहुत-से अपराध किए जाते हैं। बहुत-से मामले ऐसे हैं जिनको शरीअत ने हराम क़रार दिया है और सख़्त नापसंद किया है। सख़्त-से-सख़्त सज़ाएँ रखी हैं, वे भी लोग रज़ामंदी से ही करते हैं। जुआ खेलनेवाले रज़ामंदी से जुआ खेलते हैं। शराब पीनेवाले रज़ामंदी से शराब पीते हैं। बहुत-सी बेहयाइयाँ करनेवाले रज़ामंदी से बेहयाइयाँ करते हैं। बदकारी भी आम तौर से दोनों पक्षों की रज़ामंदी ही से की जाती है। अगर रज़ामंदी से हराम काम हलाल हो सकता तो यह तमाम मामलात पहले भी हलाल होने चाहिएँ थे और आज भी हलाल होने चाहिएँ। इसलिए यह दलील अत्यन्त बेबुनियाद, बेकार और निरर्थक बात है।
तीसरी बात एक और भी याद रखनी चाहिए, जो कुछ लोगों को ग़लत-फ़हमी में डालती है या डाल सकती है और बहुत-से लोग जान-बूझकर उसको ग़लत उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं। वह यह है कि ‘रिबा’ के हराम होने का आदेश शरीअत के बहुत-से आदेशों की तरह धीरे-धीरे करके अवतरित हुए हैं। शरीअत का यह स्वभाव रहा है कि बहुत-से सुधारों में, बहुत-से महत्वपूर्ण मामलों में, आदेश के अवतरण में क्रम से काम लिया गया है। अगर कोई आदत ख़ास तौर पर बुरी आदत लोगों में बहुत गहरे बैठी हुई थी तो उसको यक-ब-यक ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया गया। इस तदरीज की वजह यह है कि शरीअत कोई अव्यावहारिक व्यवस्था नहीं है। शरीअत की बुनियाद मात्र भावनाओं एवं अनुभूतियों या लगावों पर नहीं है। अगरचे भावनाओं, अनुभूतियों और लगावों की मानव-जीवन में बहुत महत्व है, और शरीअत भी इस महत्व का एहसास और समझ रखती है। लेकिन इंसानी मामलात में तथ्यों पर नज़र रखना, घटनाओं और मानव-जीवन के मनोविज्ञान को ध्यान में रखना, यह शरीअत के महत्वपूर्ण विशेष गुणों में से है। इन महत्वपूर्ण विशेष गुणों में क्रम से आगे बढ़ने की कार्य-प्रणाली भी है।
चुनाँचे इस उसूल को सामने रखते हुए इस्लामी शरीअत ने ‘रिबा’ के हराम होने के आदेश अवतरित किए हैं, और मक्का मुकर्रमा के ज़माने से सहाबा किराम को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। चुनाँचे सूरा-30 रूम मक्की सूरा है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के को पैग़म्बरी दिए जाने के छठे साल अवतरित हुई यानी अभी हिजरत में लगभग सात साल बाक़ी थे। मक्का मुकर्रमा के दौर के पूर्वार्ध में अवतरित होनेवाली इस सूरा में स्पष्ट रूप से इशारा किया गया कि “तुम जो रिबा का लेन-देन करते हो ताकि लोगों के माल में बढ़ोतरी हो तो यह अल्लाह की नज़र में कोई बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन जो तुम ज़कात देते हो या सदक़ात देते हो जिसका मक़सद अल्लाह की रज़ामंदी है, सो यही लोग हैं जो अपने माल में वास्तविक तौर पर बढ़ोतरी करते हैं।” (क़ुरआन, 30:39)। गोया यहाँ स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया कि ‘रिबा’ अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है। ‘रिबा’ के नतीजे में जो बढ़ोतरी माल में महसूस होती है वह अवास्तविक है, अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है। अल्लाह की नज़र में वह बढ़ोतरी पसंदीदा है जो ज़कात और सदक़ात के नतीजे में अज्रो-सवाब के रूप में सामने आती है।
इसके बाद हिजरत के तुरन्त बाद यह बताया गया कि यहूदियों को अल्लाह तआला ने ‘रिबा’ के लेन-देन से रोका था, ‘रिबा’ के निषेध का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी अवज्ञा की। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि अल्लाह की शरीअत में ‘रिबा’ पहले भी हराम था और आज भी हराम है। नापसंदीदगी पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी। शरीअत में हुर्मत (निषिद्ध होने) का पहला मरहला बता दिया गया। इसके बाद ‘रिबा’ के हराम होने का दूसरा मरहला जब अवतरित हुआ तो इसमें बताया गया कि “बढ़ता-चढ़ता सूद खाना छोड़ दो।” (क़ुरआन, 3:130)। यह ग़ज़वए-उहुद के तुरन्त बाद अवतरित होनेवाली आयत है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कम्पाउंड इंट्रेस्ट का हराम होना इस आयत के द्वारा स्पष्ट रूप से अवतरित कर दिया गया। अभी एक मरहला और बाक़ी था। जो सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) दीन को बहुत अच्छी तरह जानते थे, वे तो मक्का मुकर्रमा ही में समझ गए थे कि यह चीज़ नापसंदीदा है। कुछ और सहाबा ऐसे थे, जिन्होंने ‘रिबा’ का लेन-देन उस वक़्त से ख़त्म कर दिया जब यहूदियों के बारे में बताया गया कि उनको ‘रिबा’ से रोका गया था। बाक़ी सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने “बढ़ता-चढ़ता सूद खाना छोड़ दो।” वाली आयत के बाद सूद का लेन-देन बंद कर दिया। इक्का-दुक्का लेन-देन अब भी जारी था। ख़ास तौर पर वे लेन-देन जारी थे जिनमें पहले के क़र्ज़ों की रक़में बाक़ी थीं, या जिनमें दोनों पक्षों का ख़याल था कि उनमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। इसके बाद आख़िरी आयत सूरा-2 बक़रा की आयत नंबर-275 अवतरित हुई जिसमें हर प्रकार के ब्याज के हराम होने को स्पष्ट रूप से बता दिया गया। “अल्लाह ने तिजारत और क्रय-विक्रय को हलाल क़रार दिया है और रिबा को हराम क़रार दिया है।” यहाँ ‘अल-रिबा’ का शब्द प्रयुक्त हुआ है, ‘रिबा’ के शब्द पर (अरबी टेक्स्ट में) अलिफ़ लाम आया है जिससे यह अर्थ निकलता है कि ‘रिबा’ की हर क़िस्म को हराम क़रार दिया गया है। यहाँ अब “बढ़ता-चढ़ता” की या चक्रवृद्धि ब्याज की क़ैद नहीं है। अब हर प्रकार का ‘रिबा’ और हर प्रकार का सूद हराम क़रार दे दिया गया।
इसके बाद एक प्रकार का मरहला अभी बाक़ी था जो पहले के वाजिब क़र्ज़ों और रक़मों के बारे में था। पिछले क़र्ज़ों और बाक़ी रक़मों का यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से कुछ महीने पहले उसका हराम होना भी स्पष्ट रूप से अवतरित किया गया और यह कह दिया गया कि जितने पिछले सूद बाक़ी हैं सब आज के बाद निरस्त क़रार दिए जाते हैं। आज के बाद जिसका जो दावा चला आ रहा है वह अस्ल रक़म तक सीमित माना जाएगा।
“ऐ वे लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो तो जो रिबा बाक़ी है, किसी के ज़िम्मे क़र्ज़ है उसको छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह और रसूल की तरफ़ से एलाने-जंग सुन लो। अगर तुम तौबा कर लो तो फिर तुम्हें केवल अस्ल पूँजी लेने का हक़ है। न तुम किसी पर ज़ुल्म करो, न कोई तुम पर ज़ुल्म करे। अगर कोई व्यक्ति जिसके ज़िम्मे तुम्हारा क़र्ज़ बाक़ी है, तंग-दस्त है तो फिर बेहतर यह है उसको मोहलत दो जब तक उसे ख़ुशहाली उपलब्ध न हो जाए और अगर माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानो।”
यह आख़िरी एलान था जो सूरा-2 बक़रा की आयतें 278, 279 और 280 पर सम्मिलित है। इसका एक बार फिर फ़ाइनल और स्पष्ट रूप से एलान अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज्जतुल-विदा के अपने अभिभाषण में किया। हज्जतुल-विदा के अभिभाषण के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़िंदगी के आख़िर का बहुत महत्वपूर्ण अभिभाषण (ख़ुतबा) था जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से लगभग अस्सी दिन पहले दिया था। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का तरीक़ा यह था कि जब शरीअत का कोई आदेश अवतरित होता था तो सबसे पहले आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसपर ख़ुद अमल करते थे। ज़ाहिर है जब ‘रिबा’ के हराम होने का यह आख़िरी आदेश आया या पहला आदेश आया तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सबसे पहले उसपर भी ख़ुद अमल करके दिखाना चाहते थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कभी भी किसी सूदी कारोबार में हिस्सा नहीं लिया था, न इस्लाम से पहले और न इस्लाम के बाद। न आप के क़रीबी रिश्तेदारों में से, न आपकी बेटियों में से, न आपके अपने ख़ानदानवालों में से, न आपकी पाक बीवियों में से किसी ने सूदी कारोबार पहले किया था और न बाद में किया। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सबसे क़रीबी रिश्तेदारों में से जिनके ब्याज की रक़में लोगों के ज़िम्मे बाक़ी थीं वे हज़रत अब्बास-बिन-अब्दुल-मुत्तलिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) थे। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के चचा हज़रत अब्बास-बिन-अब्दुल-मुत्तलिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) अरब के अत्यन्त दानवीर और धनी इंसानों में थे। वह व्यापार के लिए लोगों को क़र्ज़ दिया करते थे और इस्लाम से पहले से यह सिलसिला जारी था। वे रक़में ‘मुज़ारबा’ पर भी दिया करते थे और ब्याज पर भी दिया करते थे। उनका जो क़र्ज़ होता था, वह व्यापारिक क़र्ज़ होता था, कमर्शियल इंट्रेस्ट होता था, यह ख़र्च के लिए लिया जानेवाला क़र्ज़ नहीं होता था। उनकी कुछ रक़में लोगों के ज़िम्मे बाक़ी थीं जिनमें से कुछ ग़ैर-मुस्लिम भी थे।
अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जब यह एलान किया कि मैं आज से अज्ञानकाल के तमाम दावों को निरस्त ठहरा देता हूँ। अज्ञानकाल के तमाम फ़ौजदारी प्रकार के दावे निरस्त क़रार दिए जा रहे हैं। इस मौक़े पर आपने अपने ख़ानदान के दो दावे निरस्त क़रार दिए।
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : “सबसे पहला रिबा जो में आज निरस्त क़रार दे रहा हूँ वह मेरे चचा अब्बास-बिन-अब्दुल-मुत्तलिब का रिबा है।” अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस एलान के बाद न किसी ख़र्च के लिए लिए गए क़र्ज़ पर ब्याज लेने की गुंजाइश है, न किसी व्यापारिक क़र्ज़ पर ब्याज लेने की गुंजाइश है, न पहले के बाक़ी क़र्ज़ों को जारी रखने की गुंजाइश है। ये तमाम के तमाम मामलात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हज्जतुल-विदा के मौक़े पर निरस्त क़रार दे दिए। ब्याज का हराम होना पवित्र क़ुरआन की इन आयतों में जो मैंने आपके सामने बयान कीं इतने स्पष्ट रूप से आ गया है कि अब इसमें किसी संकोच या शक की गुंजाइश नहीं रहती। जिन मुहद्दिसीन ने ‘रिबा’ के हराम होने से सम्बन्धित हदीसें बयान की हैं उनमें तमाम बड़े-बड़े मुहद्दिसीन शामिल हैं। सिहाह सित्ता की छः की छः किताबें, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नदे-इमाम अहमद, बैहक़ी की व्यापक किताब अस-सुननुल-कुबरा, इमाम तबरानी की तीनों किताबें, इमाम हाकिम की मुस्तदरक और जितनी मशहूर हदीस की किताबें हैं, ख़ास तौर पर वे हदीस की किताबें जो आदेशों को ख़ास तौर पर बयान करती हैं, इन सबमें ये हदीसें मौजूद हैं। इन हदीसों को बयान करनेवाले सहाबा की संख्या भी एक दर्जन के लगभग है। यहाँ इन हदीसों को बयान करने का तो मौक़ा नहीं है। अगर उनको बयान किया जाए तो चर्चा बहुत लम्बी हो जाएगी।
ये हदीसें सैंकड़ों नहीं तो दर्जनों ज़रूर हैं। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि सहीह मुस्लिम की रिवायत के अनुसार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ब्याज खानेवाले को, ब्याज खिलानेवाले को, ब्याज से सम्बन्धित दस्तावेज़ लिखनेवालों को, ब्याज आधारित व्यापार में गवाह बननेवालों को सबको लानत का हक़दार क़रार दिया है। और फ़रमाया कि “गुनाह में ये सब बराबर हैं।” सूदी लेन-देन में ये सब शरीक हैं। एक और रिवायत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सूदी कारोबार में शरीक होता है आख़िर में उसे अभाव और कमी का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया की बड़ी-बड़ी तिजारतें बैठ रही हैं। बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र परेशानी का शिकार हैं। दुबई में क्या हो रहा है? खरबों डालर के क़र्ज़े जो सूद और इंट्रेस्ट पर दिए गए थे वे डूब रहे हैं। बड़े-बड़े पश्चिमी देशों के बैंक एक-एककर बंद हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ बंद हो रही हैं। बड़ी-बड़ी एयरलाइन एक-दूसरे से जुड़ रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। ये सब इस हदीस में बताई गई निशानियाँ हैं जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि सूदी कारोबार बज़ाहिर जितना भी बढ़ता नज़र आए आख़िरकार सूदी कारोबार करनेवाले को अभावों और अपशगुनी का सामना करना पड़ता है।
अज्ञानकाल के ज़माने में जो सूद प्रचलित था उसमें और आज के सूद में कोई फ़र्क़ नहीं है। यह समझना कि अज्ञानकाल का सूद और था, आज का सूद और है, यह बहुत बड़ी भूल भी है और अगर कुछ लोग जान-बूझकर यह बात कहते हैं तो यह बहुत बड़ा दुस्साहस भी है। अज्ञानकाल का सूद क्या था? इसके बारे में इमाम तबरी ने एक रिवायत बयान की है, जो इतिहासकार भी हैं, टीकाकार भी, वह धर्मशास्त्री भी हैं और मुहद्दिस भी। उनकी टीका में यह रिवायत आई है और बहुत-से दूसरे लोग मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने भी इसको बयान किया है। आजकल कई लोगों ने —— और अफ़सोस कि इसमें कुछ बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं—— खींचतानकर इस रिवायत से बैंक इंट्रेस्ट को जायज़ क़रार देने की कोशिश की है। रिवायत के शब्द ये हैं कि “अज्ञानकाल में अगर किसी व्यक्ति का दूसरे के ज़िम्मे कोई क़र्ज़ बाक़ी हो, तो वह कहता था कि अगर तुम भुगतान की अवधि में मोहलत दे दो तो मैं अस्ल क़र्ज़ पर तुमको इतना या इतना बढ़ोतरी दूँगा। इसपर क़र्ज़दार और मोहलत दे दिया करता था। इसका स्पष्ट रूप से यही मतलब है कि अवधि के मुक़ाबले में अस्ल रक़म में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, और इसको ‘रिबा’ कहा जाता था। यह बढ़ोतरी चाहे जिस नाम से की जाए, जिस शीर्षक से की जाए वह सूद है।
इमाम मालिक (रह॰) का कथन उनकी मशहूर किताब ‘अल-मुदव्वनतुल-अकबरी’ में नक़्ल हुआ है। ‘अल-मुदव्वनतुल-अकबरी’ इमाम मालिक के फ़तवों पर आधारित एक बहुत बड़ा संग्रह है। एक तरह का ‘दायरुल-मआरिफ़’ है जो उनके शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों ने सामूहिक प्रयास से तैयार किया है। कई लोगों ने इसके संकलन और तैयारी में हिस्सा लिया। इसका आख़िरी और वर्तमान एडिशन इमाम अब्दुस्सलाम सहनून का संकलित किया हुआ है। यह किताब फ़िक़्हे-मालिकी की बुनियादी किताबों में से है। और इमाम मालिक (रह॰) के फ़तवों का मुवत्ता इमाम मालिक (रह॰) के बाद सबसे बड़ा मूलस्रोत है। इस किताब में इमाम मालिक (रह॰) ने ‘रिबा’ की परिभाषा करते हुए कहा है कि हर वह चीज़ जो एक निश्चित अवधि तक किसी को क़र्ज़ के तौर पर दी जाए या निश्चित अवधि के बाद चुकानी हो और उस अवधि के बाद जब वह व्यक्ति वह चीज़ अदा करे और उसके साथ कोई बढ़ोतरी भी हो तो यह बढ़ोतरी ‘रिबा’ होगी। चाहे यह बढ़ोतरी किसी ‘मशरूत’ हो या ‘मुतआरिफ़’ हो। ‘मशरूत’ से मुराद यह है कि दोनों या एक पक्ष ने शर्त रखी हो कि यह बढ़ोतरी दी जाएगी, यह शर्त लिखित हो या मौखिक दोनों स्थितियों में नाजायज़ है। ‘मुतआरिफ़’ से मुराद यह है कि यह बात आम तौर से प्रचलित और आम हो और बग़ैर लिखे या बग़ैर ज़बानी बात किए लोग इसको अदा करें।
यही बात इमाम अबू-बक्र जस्सास ने, जो मशहूर हनफ़ी फ़क़ीह भी हैं, इमामे-उसूल हैं, बड़े मुफ़स्सिरे-क़ुरआन (क़ुरआन के टीकाकार) भी हैं, अपनी किताब ‘अहकामुल-क़ुरआन’ में इस बात को लिखा है। वह कहते हैं कि जिस ‘रिबा’ से अरब के लोग परिचित थे और जिसमें वे लिप्त और मुब्तला थे वह नक़द रक़म दिरहम और दीनार के लेन-देन के बारे में था। जिसमें अवधि के मुक़ाबले में अस्ल रक़म में ज़्यादती कर दी जाती थी, बढ़ोतरी कर दी जाती थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात बताई है कि माली मामलों के लेन-देन में अवधि के मुक़ाबले में जो बढ़ोतरी की जाएगी वह दोनों पक्षों की रज़ामंदी से की जाए या बग़ैर रज़ामंदी के, वह ‘रिबा’ है। इमाम क़रतबी जो मशहूर मुफ़स्सिरे-क़ुरआन (क़ुरआन के टीकाकार) और पहली पंक्ति के मालिकी फुक़हा में से हैं, उन्होंने अपनी तफ़सीर में एक जगह लिखा है कि मुसलमानों का इस बात पर पूर्ण मतैक्य और इजमाअ है और उनके नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत और नक़्ल पर आधारित है कि क़र्ज़ में हर वह ज़्यादती या चुकाने योग्य रक़म में हर वह ज़्यादती जो मशरूत तौर पर ली जाए, चाहे वह गेहूँ की एक मुट्ठी हो या एक दाना हो वह भी ‘रिबा’ है। जानवरों के चारे की एक मुट्ठी हो या एक दाना भी होगा तो वह ज़्यादती भी ‘रिबा’ होगी। ज़्यादती कम हो या ज़्यादा हो, तुरन्त हो या उधार हो, एक साथ हो या क़िस्तों में हो, यह सबकी सब ‘रिबा’ ही की विभिन्न क़िस्में हैं।
‘रिबा’ के सन्दर्भ में फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) और मुहद्दिसीन और क़ुरआन के टीकाकारों के लेखों में क़र्ज़ का शब्द भी मिलता है और ‘दैन’ का शब्द भी मिलता है। यह बात याद रखने की है कि ‘दैन’ एक आम शब्दावली है, क़र्ज़ उसका एक प्रकार है। हर वह धन या आर्थिक ज़िम्मेदारी जो किसी के ज़िम्मे चुकानी बाक़ी हो वह ‘दैन’ कहलाती है। क़र्ज़ भी एक प्रकार का ‘दैन’ है। फुक़हा ने ‘दैन’ की परिभाषा यह की है “किसी दूसरे के लिए जो कुछ तुम्हारे ज़िम्मे अदा करना वाजिब हो वह उसका तुम्हारे ज़िम्मे ‘दैन’ है।” चूँकि क़र्ज़ ‘दैन’ की एक बहुत नुमायाँ क़िस्म है इसलिए फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) में बहुत-से लोग क़र्ज़ को ‘दैन’ के अर्थ में प्रयुक्त करते रहे हैं। और यह अरबी भाषा की एक आम शैली है जो बहुत जगह नज़र आती है कि किसी चीज़ की बहुत-सी क़िस्मों में से किसी बड़ी क़िस्म को अस्ल की जगह पर समझ लिया जाता है और सांकेतिक रूप से वह शब्द अस्ल के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगता है।
क़र्ज़ ‘दैन’ की बहुत बड़ी क़िस्म है। इसलिए दैन के लिए क़र्ज़ की शब्दावली प्रयुक्त हो जाती है। इसलिए फ़िक़्ह की किताबों से छाँट-छाँटकर मात्र उन इबारतों को निकाल लेना जहाँ क़र्ज़ का शब्द आया हो और फिर यह दावा करना कि ‘रिबा’ केवल क़र्ज़ में हो सकता है, फ़ुलाँ-फ़ुलाँ मामले में क़र्ज़ रक़म नहीं ली गई थी या देय रक़म क़र्ज़ नहीं थी। इसलिए यह सूदी मामला नहीं है, यह जहालत भी है और मामले को उलझाना भी है। अगर कोई रक़म देय है तो वह ‘दैन’ है और ‘दैन’ में जो बढ़ोतरी है या ‘दैन’ के नतीजे में जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है वह ‘रिबा’ कहलाता है।
एक मशहूर हदीस है जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “हर वह क़र्ज़ जिनके नतीजे में कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो वह ‘रिबा’ है।” ज़रूरी नहीं कि यह लाभ नक़द लाभ हो। यह किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। कुछ लोगों ने बड़े शोध और बहुत प्रयास करके यह साबित करने की कोशिश की है कि यह हदीस कलात्मक दृष्टि से हदीसे-मर्फ़ूअ नहीं है, यानी यह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मुबारक ज़बान से निकलनेवाले शब्द नहीं हैं, बल्कि किसी सहाबी का कथन है। अगर मान लीजिए यह किसी सहाबी का कथन भी है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अपने शब्द मुबारक नहीं हैं। तब भी तमाम फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) के इत्तिफ़ाक़ राय के अनुसार ऐसे तमाम कथन जो सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) से सम्बद्ध हों और जिनकी बुनियाद मात्र अक़्ल और इजतिहाद पर न हो, उनके बारे में यह समझा जाता है कि वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथन पर आधारित हैं। लेकिन इसके बावजूद शैख़ुल-इस्लाम अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) ने बहुत विस्तार से इसपर बहस की है और दलीलों से यह बात साबित किया है कि यह मर्फ़ूअ हदीस है और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपना कथन है।
इस्लाम के बड़े विद्वान और परहेज़गार लोग इस उसूल पर किस तरह अमल करते थे इसका अंदाज़ा इमाम अबू-हनीफ़ा के इस रवैये से लगाएँ। एक व्यक्ति ने उनसे कोई रक़म क़र्ज़ ली थी या इमाम साहब की कोई रक़म उसके ज़िम्मे किसी और वजह से बाक़ी थी। यह बात आपको मालूम है कि इमाम साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े व्यापारी और उद्योगपति थे। बड़े पैमाने पर लोग उनसे क़र्ज़ लिया करते थे। एक व्यक्ति ने इमाम साहब से क़र्ज़ लिया हुआ था। इमाम साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी व्यक्ति ने रोककर मसला पूछना चाहा। इमाम साहब रुककर खड़े हो गए। वह साहब जो मसला पूछना चाहते थे वह सूरज की तपन और गर्मी की वजह से एक दीवार के साये में खड़े हो गए। इमाम साहब को भी दावत दी कि दीवार के साये में आ जाएँ। इमाम साहब दीवार के साये में नहीं आए। धूप में खड़े-खड़े जवाब देते रहे। जब काफ़ी देर हुई तो उन साहब ने फिर आग्रह किया कि धूप की शिद्दत से बचने के लिए दीवार के साये में आ जाएँ। इमाम साहब फिर भी साये में नहीं आए और इसी तरह जवाब देकर चले गए। कोई शागिर्द या प्रशंसक जो साथ थे, उन्होंने पूछा कि आप उन साहब के बार-बार कहने के बावजूद दीवार के साये में क्यों खड़े नहीं हुए? इमाम ने जवाब दिया कि वह मकान जिसकी दीवार का साया था, वह मेरे फ़ुलाँ मक़रूज़ (ऋणी) का मकान था, में उसकी दीवार का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए कि वह मेरे क़र्ज़दार हैं। क़र्ज़दार की दीवार से इतना-सा फ़ायदा उठाना भी कि उसके साये में खड़े हो जाएँ इमाम साहब ने इसे हदीस के ख़िलाफ़ समझा। इससे यह अंदाज़ा होता है कि “हर वह क़र्ज़ जो लाभ ख़ींच लाए, वह रिबा है” के आदेश पर अमल करने के बारे में इस्लामी विद्वानों की रीति क्या थी, वे कितने सतर्क थे और कितनी सूक्ष्मता के साथ वे इन मामलों पर नज़र रखते थे।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि ‘रिबा’ की दो बड़ी क़िस्में थीं। एक ‘रिबाउद्दुयून’ कहलाता है दूसरा ‘रिबाउल-बुयूअ’ कहलाता है। ‘रिबाउल-बुयूअ’ आम तौर से बार्टर सेल में हुआ करता था। अब चूँकि ‘रिबाउल-बुयूअ’ उमूमन बहुत कम होता है इसलिए इस बहस का अब ज़्यादा महत्व नहीं रहा। इस बहस का महत्व अगर है तो करंसी के परस्पर लेन-देन में है या सोने चाँदी के परस्पर लेन-देन में है। ज़्यादा महत्व अब ‘रिबाउद्दुयून’ ही को हासिल है। यानी उस रक़म पर बढ़ोतरी को महत्व हासिल है जो देय रक़मों के बारे में लिया या दिया जाता है।
‘रिबाउद्दुयून’ या ‘रिबाउल-जाहिलिया’ के बारे में मैंने बताया था कि इमाम तबरी और दूसरे बहुत-से पुराने टीकाकारों और मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि ‘रिबाउद्दुयून’ की बहुत-सी शक्लें प्रचलित थीं। उनमें से एक शक्ल यह होती थी कि जब रक़म का भुगतान करने की अवधि पूरी होती थी तो क़र्ज़ देनेवाला कहता था कि या तो अस्ल रक़म अभी अदा कर दो, वर्ना फिर इसमें बढ़ोतरी क़ुबूल कर लो और आइन्दा किसी तारीख़ को भुगतान कर देता। यहाँ दो मूल तत्व होते थे। एक तो अस्ल कारोबार के आरम्भ में अस्ल रक़म पर ज़्यादती की शर्त लगा दी जाती थी। फिर क़र्ज़दार की तरफ़ से जब भुगतान में और देर होती थी तो इस देर के बदले में और बढ़ोतरी तलब की जाती था।
इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि बैंक इंट्रेस्ट में ये तीनों बातें मौजूद हैं। जब अकाउंट खोलनेवाला अस्ल रक़म जमा कराता है, उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। फिर जैसे-जैसे साल गुज़रता जाता है तो इस रक़म पर बढ़ोतरी होती जाती है। अगर पहले साल बढ़ोतरी पाँच प्रतिशत थी, दस प्रतिशत थी, सौ रुपये के एक सौ दस हो गए तो एक साल बाद इस एक सौ दस पर बढ़ोतरी मिलेगी। तीन साल के बाद एक सौ बीस पर बढ़ोतरी मिलेगी। तीन साल के बाद एक सौ तीस पर बढ़ोतरी मिलेगी। यानी और देर होने की स्थिति में और ज़्यादती होती रहती है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म क़र्ज़े होते हैं जिनमें अधिकतर व्यापारिक क़र्ज़ या कमर्शियल लोन होते हैं, उनमें तो यह बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है और वह हर द़ृष्टि से “बढ़ता-चढ़ता...” की परिभाषा में आता है। बैंक से रक़म लेनेवाला अनुबन्ध के आरम्भ ही में ज़्यादती की शर्त स्वीकार करता है। जब बैंक से लोग क़र्ज़ लेते हैं यानी पारम्परिक ब्याज आधारित बैंकों से एडवांस लेते हैं तो पहले ही दिन तय हो जाता है कि अगर दस लाख रुपये लेते हैं तो दस लाख रुपये पर बारह लाख रुपये अदा करने होंगे और जो भुगतान होता है वह बढ़ोतरी की शर्त के साथ होता है। और अगर रक़म के वापस भुगतान में विलम्ब हो तो फिर और बढ़ोतरी की शर्त रखी जाती है। अत: अगर इन दोनों के दरमियान तुलना की जाए यानी ‘रिबाउल-जाहिलिया’ का जो विवरण सीरत और हदीस की किताबों में आई हैं, उनको और बैंक इंट्रेस्ट को या बैंक से क़र्ज़ लेनेवालों के मामलों को अगर तुलना करके देखा जाए तो वे सारे तत्व जो ‘रिबाउल-जाहिलिया’ में पाए जाते थे वे सब पूर्ण रूप से मौजूद हैं और बैंक इंट्रेस्ट में पूरी तरह पाए जाते हैं। शुरू-शुरू में बैंक इंट्रेस्ट के बारे में इसकी कुछ निशानियों की वजह से कुछ विद्वानों को इस मामले में संकोच था कि यह सूद है या नहीं। बज़ाहिर बैंकों की रक़मों से कारोबार ही होता है, बज़ाहिर बैंकिंग व्यवस्था के प्रतिनिधि यही दावा करते हैं कि वे लोगों की रक़में सुरक्षित रखकर उनको व्यापार में लगाते हैं। बैंकरों के इन दावों की बुनियाद पर कुछ विद्वानों ने शुरू में इसको ब्याज मानने में संकोच किया, लेकिन विद्वानों के प्रबल बहुमत का बीसवीं सदी के आरम्भ से ही यह निश्चित फ़ैसला था कि यह ‘रिबा’ है और इसके ‘रिबा’ होने में कोई शक-सन्देह नहीं है।
हमारे उपमहाद्वीप में बीसवीं सदी के आरम्भ से, बल्कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग से महान विद्वानों ने जो फ़तवे दिए उनमें बैंक इंट्रेस्ट को सूद ही क़रार दिया गया। वक़्त के साथ-साथ जो ग़लत-फ़हमियाँ थीं वे सब एक-एककर दूर होती गईं और अब इसपर लगभग मतैक्य है कि बैंक इंट्रेस्ट ब्याज है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अरब दुनिया में कुछ लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि वह बैंक इंट्रेस्ट को ब्याज नहीं समझते। कुछ के बारे में तो यह ख़याल सही है। उदाहरणार्थ सैयद रशीद रज़ा, जिनके लेख बहुत अधिक संख्या में यहाँ भारत और पाकिस्तान में फैलाए गए। वर्तमान शैख़ुल-अज़हर, शैख़ मुहम्मद सैयद तनतावी भी बैंक इंट्रेस्ट को ‘रिबा’ नहीं समझते। ये दो नुमायाँ लोग हैं जो बैंक इंट्रस्ट को ‘रिबा’ समझने में संकोच करते हैं। तीसरा बड़ा नाम डॉक्टर अबदुर्रज़्ज़ाक़ सहनूरी का लिया जाता है जो हक़ीक़त यह है कि बीसवीं सदी के अत्यन्त सूक्ष्मता से देखनेवाले फुक़हा में से थे। उनकी गणना वर्तमान काल के बड़े-बड़े विद्वानों में होती है। उन्होंने फ़िक़्हे-इस्लामी पर एक नए अंदाज़ से बहुत शोधपरक काम किया है। उनके बारे में कुछ लोगों ने यह बार-बार दोहराया है कि वह बैंक इंट्रेस्ट को ब्याज नहीं समझते थे। यह बिलकुल ग़लत और निराधार बात है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी किताब ‘मसादिरउल-हक़ फ़िल-फ़िक़्हिल-इस्लामी’ के भाग-3 में लिखा है कि बैंक इंट्रेस्ट और इससे मिलते-जुलते दूसरे लाभ वही ‘रिबा’ है जिसको पवित्र क़ुरआन में हराम क़रार दिया गया है। ये सब लाभ ‘रिबा’ के दायरे से बाहर नहीं हैं। उन्होंने जो यह बात कही थी और यह बात उन्होंने उन्नीस सौ पचास के लगभग कही थी कि वर्तमान परिस्थितियों में बैंक इंट्रेस्ट चूँकि बहुत आम हो गया है, इसलिए फ़ौरी तौर पर इसको बिलकुल ख़त्म करना मुश्किल है। निश्चय ही उस वक़्त मुश्किल था। आज तक बहुत-से मुस्लिम देश बैंक इंट्रेस्ट को ख़त्म नहीं कर सके।
इस्लामी लोकतंत्र पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, इसमें ब्याज को ख़त्म करने की बार-बार कोशिश होती रही है और हर कोशिश बिलकुल आख़िरी मरहले पर जाकर नाकाम बना दी गई। ब्याजख़ोरी के झंडाबरदारों ने और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के पोषक लोगों ने अपनी कोशिशों और साज़िशों से उन कोशिशों को नाकाम बनाया। फिर भी यह सच है कि अब इस्लाम जगत् में इसपर सर्वसहमति हो चुकी है कि बैंक इंट्रेस्ट ‘रिबा’ ही का एक प्रकार है। बैंक इंट्रेस्ट को ‘मुज़ारबा’ समझना या मुज़ारबा की कोई क़िस्म समझना यह ‘रिबा’ की हक़ीक़त को न जानने की दलील भी है और मुज़ारबा की हक़ीक़त से बे-ख़बरी की भी। क़र्ज़, मुज़ारबा, दैन, बैंक इंट्रेस्ट, यह सब क़ानूनी या फ़िक़्ही इस्तिलाहात (पारिभाषिक शब्द) हैं। इन सबके अलग-अलग निर्धारित अर्थ हैं। इन निर्धारित अर्थों का निश्चयन क़ानून और फ़िक़्ह की किताबों के द्वारा सैकड़ों बार किया जा चुका है। इस सबको नज़र-अंदाज करके कोई साहब मात्र अपने ओहदे की धाक से, मात्र अपनी भाषण-कला या अपनी लेखन-कला से यह साबित करने का प्रयास करें कि बैंक इंट्रेस्ट ‘रिबा’ नहीं है, न केवल बहुत बड़ा दुस्साहस है, बल्कि यह एक अवैज्ञानिक ढंग है।
क़र्ज़ और दैन को इस सन्दर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। क़र्ज़ से तात्पर्य हर वह रक़म है जो किसी दूसरे व्यक्ति को इस ज़िम्मेदारी पर दी जाए कि वह निश्चित अवधि के बाद वापस कर देगा। और वह वापस कर देने का हर हालत में ज़िम्मेदार है। अगर वह रक़म उसके पास से बरबाद हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए तो भी वह वापस करने का पाबंद हो। इस रक़म को क़र्ज़ कहा जाता है। इस मामले का जो नाम भी रखा जाएगा यह क़र्ज़ ही कहलाएगा। अल्लामा इब्ने-क़ुदामा जो एक मशहूर हंबली फ़क़ीह हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे से कहे कि यह माल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इससे तिजारत करो, और उसका लाभ सारा का सारा तुम्हारा होगा तो यह क़र्ज़ कहलाएगा, उसको ‘मुज़ारबा’ हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शरीअत का बुनियादी नियम एवं सिद्धान्त है कि “मामलात में और इंसानों के दरमियान लेन-देन में अस्ल एतिबार उद्देश्यों और अर्थों का होता है, शब्दों और इबारतों का नहीं होता।”
अत: जो रक़म बैंक को दी जाती है वह क़र्ज़ है। इसलिए कि बैंक उसको अदा करने का पाबंद है। बैंक यह नहीं कह सकता कि हमारी ब्राँच में डाका पड़ गया, अत: आपके पैसे बरबाद हो गए। चूँकि बैंक यह नहीं कि सकता इसलिए उसको अमानत नहीं कहा जाएगा। अगरचे अमानत का शब्द बैंकों में बार-बार प्रयुक्त किया जाता है और अमानत के शब्द से फ़ायदा उठाते हुए उसके ‘रिबा’ होने के बारे में सन्देह पैदा किए जाते हैं। लेकिन फ़र्क़ यह है कि किसी चोरी, डाके, प्राकृतिक आपदा वग़ैरा के नतीजे में अगर रक़म बरबाद हो जाए और इस हालत में देय न हो तो वह अमानत है, देय हो तो क़र्ज़ है। अत: क़र्ज़ और दैन में बढ़ोतरी ही अस्ल और प्राचीन ‘रिबा’ है जो हमेशा से नाजायज़ और हराम समझा गया। जब भी ‘रिबा’, सूद, या ब्याज का शब्द बोला जाएगा तो इससे यही ‘रिबा’ मुराद होगा।
रिबा, रिबाउल-बुयूअ या रिबाउल-फ़ज़्ल, यह इस्लाम की शब्दावली है, और अस्ल ‘रिबा’ का रास्ता रोकने के लिए इसको हराम क़रार दिया गया है। शरीअत ने रास्ता रोकने का उसूल हर जगह सामने रखा है और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी बड़ी बुराई का रास्ता रोकने के लिए उस तरफ़ जानेवाले रास्तों की भी मनाही कर दी जाती है। इस उसूल को ‘सद्दे-ज़रिया’ (रास्ता रोकना) कहा जाता है। और यह इस्लामी शरीअत का एक निश्चित उसूल है।
रिबाउद्दुयून या रिबाउन-सैयेआ चूँकि अज्ञानकाल के ज़माने में परिचित था, मशहूर था, लोग इसको ख़ूब अच्छी तरह जानते थे, इसलिए शरीअत ने इसका विवरण और वास्तविकता को बयान करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुन्नत में ज़्यादा ध्यान ‘रिबाउल-बुयूअ’ के विवरण और वास्तविकता को स्पष्ट करने और व्याख्या करने पर दिया गया। इसलिए कि वह नई चीज़ थी, एक नई हुर्मत (निषेधाज्ञा) अवतरित हो रही थी। इसलिए हदीसों में जगह-जगह उसको स्पष्ट किया गया।
इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर (टीका) में लिखा है कि रिबाउद्दुयून या रिबाउन-सैयेआ, वही मामला है जो अज्ञानकाल में मशहूर और जाना-पहचाना था और लोग इसको जानते थे। इसकी शक्ल यह होती थी कि एक निश्चित रक़म किसी व्यक्ति को बतौर क़र्ज़ दे दिया करते थे। अस्ल रक़म बाक़ी रहती थी और एक निश्चित रक़म का भुगतान हर महीने कर दिया जाता था। यही आजकल भी हो रहा है। बैंकों के अधिकतर मामलों में यही होता है। आप पाँच लाख रुपये जमा करवा दें तो पाँच हज़ार रुपये आपको घर बैठे मिलेंगे, पाँच लाख आपके सुरक्षित रहेंगे। यही चीज़ है जिसको ‘रिबाउन-सैयेआ’ के तौर पर इमाम राज़ी ने बयान किया है। “वे लोग किसी को अपना माल दे दिया करते थे, इस शर्त पर कि हर महीने निश्चित रक़म उनको मिलती रहेगी और अस्ल पूँजी या क़र्ज़ ज्यों-का-त्यों बाक़ी रहेगा। फिर जब अस्ल पूँजी को देने का वक़्त आता था तो वह व्यक्ति या तो वह अस्ल पूँजी वापस कर दे और अगर वापस न कर सके तो फिर देय रक़म में भी बढ़ोतरी हो जाती और अवधि में भी बढ़ोतरी हो जाया करती थी।” यही वह ‘रिबा’ है जो अज्ञानकाल में जाना-माना था और अज्ञानकाल के लोग उसके अनुसार सूदी कारोबार किया करते थे।
इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि हलाल और हराम होने का ताल्लुक़ मामलात की वास्तविकता से है, शब्दों और शीर्षक से नहीं। मैं यह बात पहले भी कह चुका हूँ और यह जुमला डॉक्टर मुहम्मद अहमदुल्लाह मरहूम का है कि अस्ल महत्व शीर्षक को नहीं अन्तर्वस्तु का होता है। यही बात अल्लामा इब्ने-क़ैयिम ने एक जगह लिखी है। उन्होंने कहा है “शरीअत में और शरीअत के नियमों में इस बात पर अनगिनत तर्क एवं प्रमाण पाए जाते हैं कि मामलात में नीयत और इरादे ही का एतिबार होता है।” “इरादे का सीधे-सीधे किसी मामले के सही या ग़लत होने पर किसी मामले के जायज़ और नाजायज़ होने पर गहरा असर होता है।”
रिबाउल-बुयूअ जिसको कहा गया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यह रिबाउन-सैयेआ या रिबाउल-हदीस भी कहलाता है। इसलिए कि हदीसों के द्वारा उसको हराम क़रार दिया गया है। यह वह ‘रिबा’ है जिसको इन मशहूर हदीसों में हराम क़रार दिया गया जिनके अनुसार अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सल्लम ने बार-बार विभिन्न मजलिसों में, विभिन्न शैलियों में बयान किया। इसलिए हदीसों की किताब में यह विषय बहुत-से शब्दों में आया है कि सोने और चाँदी, गेहूँ, जौ, खजूर और नमक का आपस का लेन-देन केवल इस स्थिति में जायज़ है जब हाथ-के-हाथ हो और बग़ैर कमी-बेशी के हो। इसलिए कि अगर कमी-बेशी हुई या अवधि में देर हुई, देय अवधि बाद में रखी गई तो यह ‘रिबा’ हो जाएगा।
फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) में इसपर विस्तृत चर्चा होती रही है कि इन छः चीज़ों में क्या विशेषताएँ हैं जिनकी वजह से उनका आपस का लेन-देन इन शर्तों तक सीमित रखा गया। सोने और चाँदी के बारे में तो कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में फ़ुक़हा के दरमियान मतैक्य है कि उनमें एक जैसी बात इन दोनों का क़ीमत और ज़र (धन) होना है। इन दोनों का ज़र होना मूल आधार है। हर वह चीज़ जो ज़र की हैसियत रखती हो और लेन-देन का ज़रिया हो उसमें इस तरह की कमी-बेशी जायज़ नहीं है। चुनाँचे करंसी या करंसी के स्थान पर क्रय-विक्रय योग्य दस्तावेज़ात और वे तमाम ‘सुकूक’ और ‘तमस्सुकात’ जो दिरहमों और दीनारों की हैसियत रखते हों उन सबमें एक जैसी बात है हर वह चीज़ जो ज़र की हैसियत रखती हो उसमें कमी-बेशी और अवधि में विलम्ब जायज़ नहीं है।
मतभेद शेष चार चीज़ों के बारे में है। इसपर भी लगभग मतैक्य है। एक-आध मत जो अहले-ज़ाहिर का है वह इससे मतभेद करते हैं। कम-से-कम चारों इमामों का और तमाम बड़े फ़ुक़हा का इसपर मतैक्य है कि यह हुर्मत (निषेधाज्ञा) इन चार चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों में पाई जाएगी जिनमें वे गुण पाए जाएँगे जो इन चार चीज़ों में पाए जाते हैं। चूँकि यह चार चीज़ें मदीना मुनव्वरा में बार्टर लेन-देन का बहुत बड़ा और अहम ज़रिया थीं। यही वहाँ की पैदावार भी थीं और मदीना मुनव्वरा में बार्टर लेन-देन अक्सर इन्ही चार चीज़ों के द्वारा होता था। इसलिए हदीसों में ख़ास तौर पर उनका ज़िक्र किया गया। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) और इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) इन दोनों लोगों के नज़दीक और तमाम हनफ़ी और हंबली फ़ुक़हा के नज़दीक हर वह चीज़ जो तौलकर या गिनकर बिकती हो या नापकर बिकती हो उसपर यही शर्तें लागू की जाएँगी। हर वह चीज़ जो पापने और तौलने योग्य हो उसका आपस का लेन-देन कमी-बेशी के साथ और अवधि के विलम्ब के साथ जायज़ नहीं है। इमाम मालिक (रह॰) के नज़दीक इन चार चीज़ों में जो चीज़ समान है वह उनका भंडार किया जा सकना और खाद्य-सामग्री होना है। यानी इमाम मालिक (रह॰) के नज़दीक हर वह चीज़ जिसको इंसान भंडार कर सके, आनेवाले समय के लिए सुरक्षित रख सके और वह इंसान की रोज़ी का ज़रिया भी हो, उसका आपस का लेन-देन कमी-बेशी के साथ और अवधि के विलम्ब के साथ जायज़ नहीं है। यहाँ यह बात ज़ेहन में रखने की है कि आजकल ज़र की परिभाषा में स्टोर करने को बहुत महत्व दिया जाता है। माप और तौल से मुराद standard हो गया। गोया आजकल की शब्दावली में जो चीज़ standardized हो और जिसको store क्या जा सकता हो, store of value हो, वह भी इसमें शामिल है। इमाम शाफ़िई (रह॰) इन तीनों फुक़हा से मतभेद करते हैं। उनकी नज़र में यह उसूल तमाम खाने-पीने की चीज़ों पर लागू होगा इसलिए कि इन चार चीज़ों में समान बात यह है कि ये सब खाने की चीज़ें हैं। इसलिए हर वह चीज़ जो खाद्य-सामग्री में शामिल हो उनका आपस में क्रय-विक्रय कमी-बेशी के साथ और अवधि के विलम्ब के साथ जायज़ नहीं होगा। जो चीज़ें खाद्य-सामग्री नहीं हैं और उनमें ज़र की हैसियत भी नहीं पाई जाती, उनका आपस का क्रय-विक्रय यानी बार्टर सेल इमाम शाफ़िई (रह॰) के नज़दीक कमी-बेशी के साथ दुरुस्त है।
‘रिबा’ को शरीअत ने क्यों हराम क़रार दिया है? ‘रिबा’ के हराम होने की हिकमत (तत्वदर्शिता) क्या है? ये सवाल अगरचे एक मुसलमान को नहीं पूछने चाहिएँ, लेकिन चूँकि किसी चीज़ की हिकमत और मस्लहत (निहितार्थ) को समझ लेने से उसपर अमल करना आसान हो जाता है, इसलिए इस्लाम के बड़े इमामों ने ‘रिबा’ की ख़राबियों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। ‘रिबा’ की ख़राबियाँ नैतिक भी बयान की हैं, बुराइयाँ सामाजिक भी गिनवाई हैं और बुराइयाँ आर्थिक भी बताई हैं। इन ख़राबियों पर सबसे ज़्यादा व्यापक किताब जिस व्यक्ति ने लिखी है उसका सम्बन्ध पाकिस्तान से है।
प्रोफ़ेसर शैख़ महमूद अहमद मरहूम पाकिस्तान के मशहूर शिक्षा विशेषज्ञ थे और इस्लामी अर्थशास्त्र से उनकी दिलचस्पी बहुत पुरानी थी। उनकी दिलचस्पी के मैदान दो थे। अर्थशास्त्र और इक़बालियात। इन दोनों विषयों पर उनका महत्वपूर्ण ज्ञानपरक काम है। इस्लामी अर्थशास्त्र के विषयों में ब्याज की समस्या से उनको ख़ास दिलचस्पी थी और यह बात निजी रूप से मेरी जानकारी में है कि वे ब्याज के मसले पर कमो-बेश चालीस साल ग़ौर करते रहे, अध्ययन भी करते रहे। दूसरे विद्वानों से विचार-विमर्श भी करते रहे। मुझे भी उनसे एक दो बार विचारों का आदान-प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस लम्बे विचार-विमर्श और अध्ययन के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी Man and Money जो बड़ी व्यापक किताब है। इस किताब का एक सारांश ऑक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस ने कुछ साल पहले प्रकाशित किया है। सच तो यह है कि यह अपने विषय पर अत्यन्त ज्ञानपरक किताब है। उन्होंने इस किताब में इतिहास, धर्म, अर्थव्यवस्था, दर्शन, गणित, ग़रज़ हर कला के तर्कों से यह साबित किया है कि ‘रिबा’ की तमाम क़िस्में और शक्लें वे तमाम ख़राबियाँ रखती हैं जो इस्लामी समाज के आधार को बिगाड़ने के समान हैं। मैं पूरी ईमानदारी और पूरे विवेक से यह समझता हूँ कि प्रोफ़ेसर शैख़ महमूद अहमद मरहूम की यह किताब आधुनिक इस्लामी अर्थशास्त्र के इतिहास में वही हैसियत रखती है जो इमाम ग़ज़ाली की किताब ‘तहाफ़तुल-फ़िलासफ़ा’ इस्लामी लिट्रेचर के प्राचीन इतिहास में रखती है।
सूद की ख़राबियाँ पहले के उलमा ने भी बयान की हैं, बादवालों ने भी बयान की हैं। पवित्र क़ुरआन की आयत “अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदक़ात को बढ़ाता है” की टीका में बहुत-से टीकाकारों ने उन ख़राबियों का ज़िक्र किया है। अल्लाह तआला सूद को ख़त्म करता और मिटाता है। सूद की नतीजे में जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता नज़र आता है, अल्लाह तआला उसके रास्ते में रुकावट डालता है, और सदक़ात में बढ़ोतरी करता है। इसकी व्याख्या में टीकाकारों ने जो लिखा है उसका सार यह है कि ब्याज आख़िरकार पतन का कारण होता है। ब्याज के नतीजे में अस्थायी विकास तो बहुत हो जाता है। बज़ाहिर ख़ुशहाली क़ायम हो जाती है। लेकिन आख़िरकार अर्थव्यवस्थाएँ तबाही का शिकार हो जाती हैं। यह तबाही कभी तो बहुत जल्दी आ जाती है, चालीस पचास साल बाद ही आ जाती है। कभी उसके आने में समय लगता है, सौ-दो-सौ साल लगते हैं। आजकल चूँकि बहुत बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हो गई हैं। खरबों डॉलर पर बनी अर्थव्यवस्थाएँ क़ायम हैं, बल्कि इतने डॉलर और पौंडों पर बनी हैं जिनको गिनने के लिए उर्दू में अंक नहीं है। सैंकड़ों हज़ारों खरब डालर पर आधारित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इसलिए इन बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बैठने में वक़्त लगता है। छोटी कश्ती या नाव जल्दी डूब जाती है। बड़ा जहाज़ डूबने में भी महीना और हफ़्ता लगता है। लेकिन डूबना आख़िरकार सूदी अर्थव्यवस्था के बादबानों से चलनेवाली कश्ती का मुक़द्दर होता है।
सूद आर्थिक इंसाफ़ के रास्ते में बहुत बड़ी बल्कि शायद सबसे बड़ी रुकावट है। पवित्र क़ुरआन ने आदेश दिया था कि धन का संकेन्द्रण एक वर्ग में नहीं होना चाहिए। “ऐसा न हो कि दौलत तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही घूमती रहे।” (क़ुरआन, 59:7) सूद इस आदेश के रास्ते में स्पष्ट रूप से रुकावट है। सूद के नतीजे में दौलत का संकेन्द्रण होता है। सूद पवित्र क़ुरआन के इस स्पष्ट आदेश से टकराता है। सूद के नतीजे में आर्थिक न्याय ख़त्म हो जाता है। आर्थिक न्याय के रास्ते में जो बड़ी-बड़ी रुकावटें हैं उनमें से एक सूदी कारोबार और लेन-देन भी है। सोदी कारोबार में ट्रेड साइकिल अपरिहार्य है। हर व्यवस्था में जो सूद पर चलती हो एक ट्रेड साईकिल यानी तिजारती चक्कर का पैदा होना अपरिहार्य होता है। एक समय आता है कि चक्कर पूरा होता है और तबाही आ जाती है। फिर दूसरा चक्कर शुरू होता है। फिर उसका नतीजा ख़राबी की शक्ल में निकलता है। फिर तीसरा चक्कर शुरू होता है। ख़ुद पश्चिमी अर्थव्यवस्था का इतिहास विकास के इन सारे दावों के बावजूद और इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद इस वास्तविकता का गवाह है। इसमें पिछले सौ पचास सालों में जो-जो चक्कर आए हैं वे हम सबके सामने हैं। और ज़्यादा ख़राबी जो पैदा होती है वो fiat money के द्वारा पैदा होती है। फ़िएट मनी यानी काग़ज़ी करंसी या फ़र्ज़ी ज़र, ज़रे-काग़ज़ी और सूद, यह दोनों मिलकर क़ियामत बरपा कर डालते हैं। काग़ज़ी करंसी एक तो वह होती है जो राज्य जारी करता है। वह फिर ग़नीमत है। उसकी ख़राबियाँ भी तुलनात्मक रूप से कम हैं। लेकिन एक काग़ज़ी करंसी वह होती है जो राज्य जारी नहीं करता, लेकिन उसकी हैसियत भी व्यावहारिक रूप से काग़ज़ी करंसी की हो जाती है। जो काग़ज़ात क्रय-विक्रय के योग्य होते हैं, जिनके पीछे अस्ल रक़म तो केवल नाम मात्र होती है। कभी-कभी पाँच प्रतिशत भी नहीं होती। पाँच प्रतिशत रक़म के मुक़ाबले में सौ प्रतिशत मात्र काग़ज़ों और व्यापारिक दस्तावेज़ात की बुनियाद पर कारोबार हो रहा होता है। अगर कहीं से इस पाँच प्रतिशत को नुक़्सान हो जाए तो वह 95 प्रतिशत कारोबार तुरन्त बुरी तरह बैठ जाता है। चूँकि सारी रक़म फ़र्ज़ी रक़म होती है। काग़ज़ी तौर पर दोगुनी से चार गुनी, चार गुनी, आठ गुनी, सोलह गुनी और इस तरह सैंकड़ों गुनी होती चली जाती है इसलिए डूबती भी बहुत जल्दी है। लोगों को यह तरक़्क़ी तो बहुत नज़र आती है, लेकिन अगर इस तरक़्क़ी के ग़ुब्बारे में कहीं छेद हो जाए तो उसके नतीजे में पलक झपकते ही यह सारा ग़ुब्बारा बुलबुले की तरह बैठ जाता है। यह पवित्र क़ुरआन की इस आयत की स्पष्ट व्याख्या है। “अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदक़ात को बढ़ाता है।”
फिर ‘रिबा’ की ख़राबियाँ केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप अगर व्यक्तियों के दरमियान हो, ख़ास तौर पर आपस में जो कपट और दुश्मनी पैदा होती है वह एक स्पष्ट सच है। जहाँ व्यक्तियों के दरमियान खींचातानी और कपट और वैर का पैदा होना एक ऐसी हक़ीक़त है जिससे वही व्यक्ति इनकार कर सकता है जो ब्याजख़ोरी में चरम सीमा तक पहुँच गया हो।
पवित्र क़ुरआन ने जिस ‘मारूफ़’ का आदेश दिया है वह ‘मारूफ़’ सूद के नतीजे में ख़त्म हो जाता। है। पवित्र क़ुरआन जिस लेन-देन का आदेश देता है उस की बुनियाद आपस में भाईचारे पर, मुहब्बत पर, तकाफ़ुल (परस्पर आर्थिक सहयोग) पर, हमदर्दी और समानता पर होनी चाहिए। यह धारणाएँ ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था में निरर्थक हैं। ब्याज जगत् में इन धारणाओं को एक समय हुआ निष्कासित किया जा चुका है। भ्रातृत्व भाव से परस्पर सहयोग स्वार्थपरता के इस वातावरण में अकल्पनीय होता है। ब्याजख़ोर का रवैया अमानवीय रवैया होता है। उसको इससे बहस नहीं होती। न अतीत के हिंदू ब्याजख़ोर बनिए को कोई मतलब होता था, न वर्तमान समय के संस्थागत यानी institutional ब्याजख़ोर को इससे कोई मतलब होता है कि क़र्ज़दार पर क्या गुज़र रही है और उसका कारोबार किस हाल में है। इंसानी रवैया इस पूरे कारोबार में कोई हैसियत नहीं रखता। फिर एक ख़ास बात जो बहुत-से अर्थशास्त्रियों ने लिखी है, वह यह है कि ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था के नतीजे में बेरोज़गारी और बेकारी बढ़ जाती है। जहाँ कोई व्यापार काम कर रहा हो, कोई उद्योग वास्तविक रुप से लगाया जा रहा हो, कोई वाक़ई तरक़्क़ी हो रही हो, जिसके नतीजे में अस्ल पूँजियाँ पैदा हो रही हों, वहाँ तो व्यापारिक गतिविधियाँ फैलती हैं और बढ़ती हैं। इसके नतीजे में दौलत की गर्दिश भी तेज़ होती है, दौलत का फैलाव भी आम होता है और रोज़गार के नए-नए अवसर भी पैदा होते जाते हैं। लेकिन जहाँ सारा विकास फ़र्ज़ी और काग़ज़ी हो वहाँ रोज़गार के नए अवसर पैदा होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कि जहाँ न वास्तविक उद्योग है, न वास्तविक व्यापार है, न वास्तविक सेवाएँ पैदा हो रही हैं तो वहाँ रोज़गार कहाँ से पैदा होगा?
फिर जो व्यक्ति सूदी रक़म खाने का आदी हो जाता है उसके स्वभाव में काम और मेहनत से दूर भागने की आदत पैदा हो जाती है। अगर सूद खानेवाले को घर बैठे दौलत मिल रही हो तो उसको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। उसको दिमाग़ लगाने की क्या ज़रूरत है। उसे नये उद्योग और इंडस्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है। यह सब सिरदर्द बढ़ाने के काम हैं। वह जुए से और ब्याजख़ोरी से और दौलत पैदा करता चला जाएगा। और लोगों की जेबों पर डाका डालता चला जाएगा।
फिर ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था जहाँ-जहाँ फैलती है वहाँ व्यापार के प्रति अलगाव पैदा होता है। उद्योग और खेती की ओर से ध्यान हट जाता है। चुनाँचे इसका स्पष्ट उदाहरण है कि जो लोग ब्याज खाने में ज़्यादा नुमायाँ हैं वे न खेती में दिलचस्पी रखते हैं, न उद्योग में, न व्यापार में, इसलिए कि उनको खेती से इतनी आय नहीं होती, उद्योग से इतनी आय नहीं होती, तिजारत से इतनी आय नहीं होती जितनी आय घर बैठे ब्याज के नतीजे में हो जाती है।
इसके अलावा यह तो हर व्यक्ति मानता है कि ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था ज़रूरतमंद की ज़रूरत का शोषण है, ख़ास तौर पर अगर सूदी क़र्ज़ ख़र्च के लिए लिया गया हो, निजी और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए हो। इसमें तो शोषण के होने पर ख़ुद ब्याज खानेवाले भी सहमत हैं और मानते हैं कि यह शोषण का एक ज़रिया है। लेकिन जो तिजारती क़र्ज़े हैं वहाँ भी घोर शोषण का प्रभाव पाया जाता है। शरीअत का स्वभाव यह है कि व्यापार और कारोबार लोगों की आपस की रज़ामंदी से हो। साफ़-सुथरे अंदाज़ से हो। न्याय और इंसाफ़ के साथ हो। हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। जो जितनी पूँजी लगाए उतना लाभ उसको मिले। एक व्यक्ति अपनी मेहनत दाँव पर लगाए, दूसरा व्यक्ति अपनी पूँजी दाव पर लगाए। दोनों की कोई न कोई चीज़ दाव पर लगी हो और दोनों की कोशिशों से जो व्यापार या कारोबार या मशीनरी चले, फिर उसका लाभ सन्तुलन और न्याय के साथ उचित ढंग से बँटना चाहिए।
शरीअत ने ‘ग़बने-फ़ाहिश’ को हराम क़रार दिया है। ‘ग़बने-फ़ाहिश’ से मुराद नफ़ाख़ोरी की वह स्थिति है जो बाज़ार के आम रिवाज और भाव से इतनी अलग हो कि उसका अंदाज़ा लगानेवाले अंदाज़ा न लगा सकें। इसके विभिन्न स्पष्टीकरण फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने अपने-अपने ज़माने के चलन की दृष्टि से किए हैं। उदाहरणार्थ ज़मीन और जायदाद की क़ीमत में अगर बढ़ोतरी बीस प्रतिशत से अधिक हो तो समझा जाएगा कि यह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है। एक ज़मीन किसी जगह एक लाख रुपये प्रति कनाल मिलती है। वहाँ कोई व्यक्ति एक लाख बीस हज़ार की बेचेगा तो समझा जाइएगा कि ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है। एक लाख पाँच हज़ार, एक लाख दस हज़ार का फ़र्क़ गवारा समझा गया। इसलिए कि इतना फ़र्क़ तो स्वाभाविक है और इस तरह के कारोबार में होता है। इस मिसाल से यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि ‘ग़बने-फ़ाहिश’ से मुराद नफ़ाख़ोरी का वह रूप है जो न्याय और इंसाफ़ की प्रचलित धारणाओं और शरीअत के आदेशों से टकराता हो।
वर्तमान रिबा-व्यवस्था में और सूदी-व्यवस्था में जगह-जगह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ की बुराई पाई जाती है। अगर एक व्यक्ति बैंक से क़र्ज़ लेता है और उसका कारोबार या उद्योग ख़ूब चलता है, लेकिन वह बैंक को दस प्रतिशत, बारह प्रतिशत ब्याज दे रहा है, तो यह भी ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है। इसलिए कि अगर यह साझेदारी है तो साझेदारी में दोनों पक्षों के लाभ में कोई अनुकूलता होनी चाहिए। एक व्यक्ति सौ रुपये के दो सौ कमा रहा है। ख़ुद नव्वे रखता है दूसरे को दस देता है। यह निश्चय ही ‘ग़बने-फ़ाहिश’ है।
उद्योग के कुछ प्रकार वे हैं जिनमें लाभ की दर इससे भी ज़्यादा होती है। एक बार चमड़े के एक बड़े विशेषज्ञ ने मुझे बताया था। वह चमड़े के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, दुनिया-भर में चमड़ा बनाने के मामलों में मश्वरे के लिए बुलाए जाते थे। उन्होंने एक बार बताया था कि यहाँ जो जूता बनता है, बाटा कंपनी बनाती है। इसकी मालियत डेढ़ या दो रुपये से ज़्यादा नहीं होती। यह बात मुझे उन्होंने सन् 1980 में बताई थी। बाटा कंपनी इस जूते को उस ज़माने में कम-से-कम चालीस पचास रुपये से लेकर सौ डेढ़ सौ रुपये में बेचती थी। अगर उनका यह अंदाज़ा दुरुस्त था, इस तरह के और अंदाज़े भी मैंने सुने हैं जो विशेषज्ञों ने बताए हैं तो इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि ‘ग़बने-फ़ाहिश’ की एक शक्ल यह भी है कि बैंक और बैंक के हज़ारों खातेदारों को उनके दस बारह प्रतिशत ब्याज पर सन्तुष्ट करके बिठा दिया जाए और बाक़ी जितना लाभ हो वह सारा का सारा एक पक्ष के पास चला जाए।
यह ‘ग़बने-फ़ाहिश’ की मात्र एक क़िस्म है। दूसरी किस्में और शक्लें ‘ग़बने-फ़ाहिश’ की और भी हो सकती हैं। ये वे कुछ अहम ख़राबियाँ हैं जो ब्याज में पाई जाती हैं जिनकी वजह से शरीअत ने ब्याज को नाजायज़ और व्यापार को जायज़ क़रार दिया है। ‘रिबा’ और ‘बैअ’ दोनों को शरीअत ने एक साथ बयान किया है। जहाँ ‘रिबा’ को हराम क़रार दिया है वहाँ ‘बैअ’ को उसके विकल्प के रूप में बयान किया है। गोया ‘रिबा’ का वास्तविक विकल्प व्यापार है। व्यापार में लेन-देन और कारोबार की वे तमाम शक्लें शामिल हैं जो न्याय और इंसाफ़ के अनुसार हों और जिनकी शरीअत ने अनुमति दी हो। जिनमें लाभ-हानि में समान रूप से साझेदारी पाई जाती हो। जिनमें किसी पक्ष का हक़ प्रभावित न हो। किसी पक्ष को नाजायज़ जमाख़ोरी या नाजायज़ नफ़ाख़ोरी का मौक़ा न हो। जिसके नतीजे में समाज में वास्तविक व्यापार, वास्तविक उद्योग या वास्तविक पूँजियाँ पैदा हो रही हों। जिसके नतीजे में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हों। जिसके नतीजे में आर्थिक विकास हो रहा हो और होता नज़र आ रहा हो।
ये सब मामले तिजारत और बैअ में निश्चित रूप से होते हैं। ‘रिबा’ और ‘बैअ’ में ज़मीन आसमान का अन्तर है। पवित्र क़ुरआन में एक वाक्य में इन तमाम ख़राबियों को नाजायज़ क़रार दिया गया जिनमें से कुछ की मैंने निशानदेही की और उन तमाम ख़ूबियों को पसंदीदा कहा गया जो व्यापार में पाई जाती हैं। इससे पहले व्यापार पर चर्चा करते हुए मैं यह बात कह चुका हूँ कि व्यापार पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) का पेशा रहा है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक ईमानदार व्यापारी थे। आपके बड़े सहाबा ईमानदार व्यापारी थे। चूँकि आपकी लाई हुई शरीअत को एक ऐसे दौर में विश्व-व्यवस्था के रूप में सामने आना था, जहाँ वैश्विक व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था का दौर होगा, जहाँ globalized economy का दौर-दौरा होगा। वहाँ व्यापार के आधार पर जो आर्थिक विकास जन्म लेगा वही सफल रहेगा। ‘रिबा’ के आधार पर जो अर्थव्यवस्ता बनेगी वह असफल रहेगी। इसलिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की लाई हुई शरीअत ने पहले दिन से व्यापार को महत्व दिया और उसके न्यायपूर्ण आदेश विस्तार से प्रदान किए। यही सार है आज की चर्चा का।
Recent posts
-

इस्लाम में अर्थव्यवस्था एवं व्यापार का महत्व तथा उसके आदेश (लेक्चर-6)
20 January 2026 -

इस्लाम में धन-सम्पत्ति एवं स्वामित्व के आदेश (लेक्चर-5)
06 January 2026 -

अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में राज्य की भूमिका (लैक्चर-4)
23 December 2025 -

आधुनिक काल की मुख्य वित्तीय एवं आर्थिक समस्याएँ : एक अवलोकन (लैक्चर-3)
18 December 2025 -

इस्लाम की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था मूल-अवधारणाएँ, महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा लक्ष्य (लैक्चर -2)
16 December 2025 -
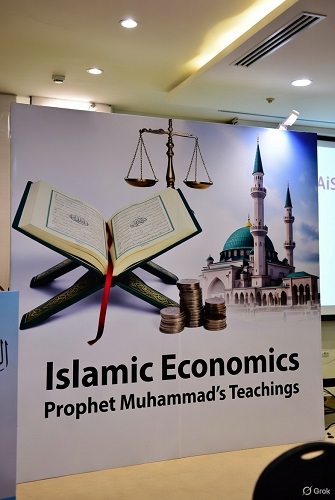
वित्त और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत पवित्र कुरआन और पैगंबर हजरत मोहम्मद (स0) की सुन्नत (शिक्षाओं एवं निर्देशों) की रोशनी में! (लैक्चर -1)
10 December 2025

