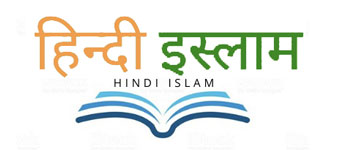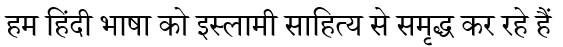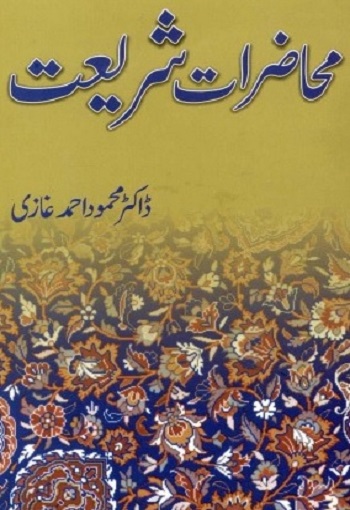
इस्लामी शरीअत : एक परिचय (शरीअत: लेक्चर #1)
-
शरीअत
- at 07 August 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
दो शब्द
लेक्चर्स के इस सिलसिले का पाँचवाँ भाग ‘मुहाज़राते-शरीअत’ पाठकों की सेवा में पेश है। दिल, ज़बान और क़लम उस अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करने में असमर्थ हैं जिसकी मेहरबानी और कृपा से यह तुच्छ-सी सेवा सम्भव हो सकी। इन लेक्चर्स (मुहाज़रात) में कोशिश की है कि इस्लामी शरीअत का एक व्यापक और भरपूर परिचय पेश किया जाए और इसके मौलिक तत्त्वों और अध्यायों को ठीक-ठीक इसी तरह पेश किया जाए जिस प्रकार इस्लामी इतिहास के प्रमाणित, विश्वसनीय और भरोसेमन्द फुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों), मुतकल्लिमीन (इस्लामी धारणाओं को बौद्धिक तर्कों से सिद्ध करनेवालों) और अस्हाबे-तज़किया (आन्तरिक शुद्धि करनेवालों) ने इसको समझा और बयान किया है। जहाँ-जहाँ शरीअत के पक्ष को समझने में कुछ लोगों से गलतियाँ हुई हैं या शरीअत की शिक्षा और नियमों तथा आदेशों के बारे में कुछ क्षेत्रों में किसी प्रकार की ग़लत-फ़हमियाँ या उलझनें पाई जाती हैं उनको दूर करने की भी हर सम्भव कोशिश की गई है।
शरीअत के आम और व्यापक परिचय के साथ यह बात भी सायास सामने रखी गई है कि शरीअत को मात्र वैचारिक ढंग से न देखा जाए और इसको किसी शून्य में बयान करने का प्रयास न किया जाए, बल्कि शरीअत को मुस्लिम समाज के विश्वव्यापी और अन्तर्पीढ़ीगत (intergenerational) भूमिका की पृष्ठभूमि में देखा, समझा और बयान किया जाए और इस्लामी शरीअत को मुस्लिम समाज की सबसे प्रभावशाली, सबसे सशक्त और सबसे ज़्यादा व्यापक प्रेरक शक्ति के तौर पर नुमायाँ किया जाए।
ये लेक्चर्स इस्लामाबाद और दोहा क़तर की विभिन्न सभाओं में विभिन्न समयों में पेश किए गए थे। इन सभाओं में अन्तराल भी बहुत लम्बे आते रहे और श्रोता भी बदलते रहे। इसलिए कुछ विषयों की पुनरावृत्ति हो गई है। चूँकि यह पुनरावृत्ति कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में है इसलिए इसको दूर करने की कोशिश नहीं की गई। उम्मीद है कि पाठक किताब और लेखक की इस कमज़ोरी को भी दूसरी बहुत-सी कमज़ोरियों की तरह अनदेखा कर देंगे।
इन लेक्चर्स में कुछ का पहला संस्करण इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ़ पालिसी स्टडीज़ में जनवरी 2008 ई॰ में पेश किया गया था। अलबत्ता इस संग्रह में अनगिनत लेक्चर्स वे हैं जो दोहा, क़तर की संक्षिप्त और सीमित सभाओं में पेश किए गए थे। इन स्वाभाविक लेक्चर्स को टेप रिकार्डर से काग़ज़ पर लिखने का काम मेरी प्यारी बेटी हाफ़िज़ा हफ़्सा ज़ैनब ग़ाज़ी ने बहुत मेहनत और लगन से किया। अल्लाह तआला उसको इसका उत्तम प्रतिदान प्रदान करे और इस प्रयास को उसके लिए आख़िरत में काम आनेवाला भंडार बनाए।
इस सिलसिले का आरम्भ मेरी मरहूमा बहन अज़्रा नसीम फ़ारूक़ी के प्रस्ताव और आग्रह पर हुआ था। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस तुच्छ लेखक और इस सिलसिले का सबसे पहले प्रस्ताव देनेवाली दोनों व्यक्तियों को अपनी दुआओं में न भूलें।
महमूद अहमद ग़ाज़ी
दोहा (क़तर)
Aug 26, 2009
5 रमज़ानुल-मुबारक 1430 हि॰
लेक्चर नम्बर-1
आधुनिक काल में इस्लाम की बहुत-सी शब्दावलियों और शिक्षाओं के बारे में ग़लत-फ़हमियों का एक व्यापक सैलाब उमड़ता हुआ महसूस होता है। पिछले दो-ढाई सौ वर्षों के दौरान जब से मुस्लिम जगत् का प्रत्यक्ष सम्पर्क विभिन्न उपनिवेशवादी शक्तियों से पड़ा है उस समय से यह ग़लत-फ़हमियाँ पैदा हो रही हैं, बल्कि सायास पैदा की जा रही हैं। जिस ज़माने में जो ग़लत-फ़हमी पैदा होती है उस ज़माने की राजनैतिक परिस्थितियों पर नज़र डाली जाए तो उस ग़लत-फ़हमी के कारण और प्रेरक बहुत आसानी से सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब अठारहवीं शताब्दी के मध्य में मुस्लिम जगत् के अधिकांश देश पश्चिमी उपनिवेशवाद को विस्तार देने सम्बन्धी लक्ष्य का निशाना बने तो हर जगह पश्चिमी शक्तियों को इस्लाम के लिए संघर्ष करनेवालों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हर जगह इस्लाम के लिए संघर्ष करनेवाले निष्ठावान इस्लामी विद्वानों के निर्देशन में पूरी तैयारी से मुस्लिम जगत् के बचाव के लिए मैदान में आ गए।
इंडोनेशिया के इमाम बोंजोल से लेकर मराक़श (मोरक्को) के अमीर अब्दुल-क़ादिर अल-जज़ाइरी तक, दाग़िस्तान के इमाम शामिल से लेकर सोमालिया के इमाम मुहम्मद-बिन-अब्दुल्लाह अल-सुन्नी के प्रयासों तक हर जगह एक ही दृश्य और एक ही नक़्शा नज़र आता है। ये सब लोग तलवार लेकर विदेशी हमलावर के ख़िलाफ़ पंक्तिबद्ध हुए और दारुल-इस्लाम की आज़ादी और इस्लामी जीवन-शैली की सुरक्षा के लिए जानों का नज़राना पेश किया। संघर्ष का यह सिलसिला वर्षों जारी रहा और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक कमो-बेश 150 वर्ष का ये लम्बा अरसा एक भरपूर और निरन्तर संघर्ष का समय क़रार दिया जा सकता है।
इन हालात में पश्चिमी लेखकों ने जिहाद और मुजाहिदीन के बारे में ग़लत-फ़हमियाँ पैदा करना ज़रूरी समझा, उस ज़माने से पश्चिमी लेखक और उनके पूर्वी प्रशंसक जिहाद के बारे में ग़लत-फ़हमियाँ पैदा करते आ रहे हैं।
इसी तरह जब पश्चिमी उपनिवेशवाद के साथ में ईसाई पादरियों की बड़ी संख्या मुस्लिम जगत् में आई और मुसलमानों को इस्लाम से फेर देने के प्रयास ज़ोर-शोर से शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि उनके ये प्रयास सरासर असफलता का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने इस असफलता के कारणों पर विचार किया तो उनको आभास हुआ कि मुसलमानों में इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेना अत्यन्त बुरा समझा जाता है। यह बात न केवल सामाजिक स्तर पर अत्यन्त अप्रिय समझी जाती है जिसके नतीजे में इस्लाम छोड़नेवाला अपने समाज से पूरे तौर पर कट जाता है, बल्कि यह हरकत एक गंभीर फ़ौजदारी अपराध की हैसियत भी रखती है, जिसकी सज़ा फ़िक़्हे-इस्लामी के अनुसार मौत है। यह अपराध वस्तुतः राज्य के आधार के ख़िलाफ़ महाविद्रोह का अपराध समझा जाता है जिसकी अनुमति इस्लामी राज्य में नहीं दी जाती।
पश्चिमी विद्वानों ने और विशेष रूप से प्राच्यविदों ने जब से इस बात को महसूस किया, उस वक़्त से अपना यह फ़र्ज़ क़रार दे दिया कि इस्लाम से निकलने की सज़ा के बारे में ग़लत-फ़हमियाँ पैदा करते जाएँ और ऐसे-ऐसे सवाल, सन्देह और आपत्तियाँ उठाते चले जाएँ जो मुस्लिम समाज में पैदा नहीं होनी चाहिएँ।
इसी तरह जब उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से यह बात महसूस होनी शुरू हुई कि अब सल्तनते-उस्मानिया का पतन अपनी आख़िरी हदों को पहुँचनेवाला है। उस समय से पश्चिमी शक्तियों के दरमियान जहाँ यह प्रतिस्पर्धा शुरू हुई कि सल्तनते-उस्मानिया के अधिकृत क्षेत्रों पर कौन क़ब्ज़ा करे, वहाँ यह दौड़ भी शुरू हुई कि ख़ुद ‘ख़िलाफ़त’ की संस्था को भी बदनाम किया जाए, ख़िलाफ़त को मुसलमानों की समस्याओं और मुश्किलों का कारण ठहरा दिया जाए, अरब मुसलमानों के दिलों में तुर्कों के ख़िलाफ़ विरोधपूर्ण भावनाएँ पैदा की जाएँ और मुसलमानों की एकता और सामुदायिक एकजुटता को एक अवास्तविक और अस्पष्ट चीज़ ठहराया जाए। चुनाँचे दुनिया भर के मुसलमानों की दीनी एकता और सामुदायिक एकजुटता के ख़िलाफ़ जनाधार तैयार करने के लिए ‘पान इस्लामिज़्म’ की शब्दावली गढ़ी गई और इस शब्दावली के पर्दे में इस्लामी एकता को निशाना बनाया गया जिसका स्पष्ट उद्देश्य इस्लामी ख़िलाफ़त को निशाना बनाना था। इन कुछ मिसालों से यह बात दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो जाती है कि इस्लामी शब्दावलियों और इस्लामी धारणाओं के बारे में बहुत-से पश्चिमी विद्वानों के बज़ाहिर बौद्धिक प्रयास राजनैतिक प्रेरकों से ख़ाली नहीं होते। पश्चिम के नीति निर्माता जब अपने राजनैतिक और सैन्य निहितार्थों के तहत ज़रूरी समझते हैं तो विभिन्न इस्लामी शब्दावलियों को निशाना बनाते हैं। प्रायः आरम्भिक क़दम के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से इस्लामी शब्दावली को निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि पहले उसके लिए कोई और शब्दावली प्रस्तावित की जाती है जो आम तौर से किसी पश्चिमी भाषा के शब्दों पर आधारित होती है। कुछ समय इस नई स्वरचित शब्दावली को आलोचना और उपहास का निशाना बनाया जाता है। धीरे-धीरे जब ज़ेहन तैयार हो जाते हैं तो फिर अस्ल इस्लामी शब्दावली पर और फिर सम्बन्धित इस्लामी शिक्षाओं पर हमला किया जाता है। यह सिलसिला पिछले दो सौ वर्षों से लगातार जारी है।
पिछले कुछ दशकों से जो शब्दावली आलोचना और उपहास का निशाना बनाई जा रही है वह ख़ुद ‘शरीअत’ की शब्दावली है। शरीअत के बारे में बहुत-सी ग़लत-फ़हमियाँ पैदा हो गई हैं या पैदा कर दी गई हैं। इन ग़लत-फ़हमियों के पैदा करने में पश्चिमवालों के साथ-साथ नादान और नासमझ मुसलमानों का हिस्सा भी कम नहीं। शरीअत का शब्द जितना आम है उतना ही उसके बारे में ग़लत-फ़हमियाँ भी आम हैं। पश्चिमवालों का एक बहुत बड़ा वर्ग शरीअत को कुछ रूढ़िवादी आदिवासी परम्पराओं का एक संग्रह समझता है। पश्चिमी संचार माध्यमों से जुड़े कुछ लोगों ने इस विचार को बहुत फैलाया है कि शरीअत से अभिप्रेत अरब के प्राचीन आदिवासी तौर-तरीक़े हैं जिनको मुसलमान आज इक्कीसवीं शताब्दी में ज़िन्दा करना चाहते हैं। इस प्रभाव के पैदा करने में पत्रकारों के साथ-साथ नामवर पश्चिमी शोधकर्ताओं और प्राच्यविदों का हिस्सा भी कम नहीं। गोल्ड तसीहर, जोज़ेफ़ शाख्त (Joseph Schacht) जैसे नामवर विद्वानों ने सुन्नत को अज्ञानकाल के प्राचीन तौर-तरीक़ों का संग्रह साबित करने की कोशिश की। इन प्राच्यविदों के कई पूर्वी श्रद्धालुओं ने इन्हीं विचारों को दोहराते हुए यह विचार मुस्लिम जगत् में भी परिचित करा दिए। ज़ाहिर है कि जब शरीअत के एक अति महत्त्वपूर्ण स्रोत को पूरे का पूरा अज्ञानकाल के तौर-तरीक़ों से लिया हुआ क़रार दे दिया जाए तो फिर अगला चरण मुश्किल नहीं रहता।
शरीअत के बारे में कुछ ग़लत-फ़हमियाँ मुस्लिम जगत् में मौजूद सेक्युलर वर्ग में भी पाई जाती हैं। यह वर्ग अगरचे संख्या में बहुत सीमित है, लेकिन अपने प्रभाव एवं पहुँच की दृष्टि से बहुत ताक़तवर और प्रभावशाली है। इस वर्ग के विचार में शरीअत मध्य युग की एक प्राचीन धार्मिक व्यवस्था है जो अब अपनी उपयोगिता खो चुकी है। इस वर्ग के विचार में दुनिया अब रौशन ख़याली के दौर में दाख़िल हो चुकी है। इस रौशन ख़याल दौर में मध्य युग का चला हुआ कारतूस इस्तेमाल करने की कोशिश करना बेवक़ूफ़ी है। यह वर्ग इस्लामी इतिहास, इस्लामी संस्कृति और इस्लामी सभ्यता से आम तौर पर पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। अव्वल तो इस वर्ग में इस्लाम, इस्लामी शिक्षा, इस्लामी इतिहास और इस्लामी सभ्यता से अवगत होने की कोई भावना नहीं पाई जाती, और यह अपने वैचारिक स्वरूप, शैक्षिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक उठान की दृष्टि से आम पश्चिमवालों से भिन्न नहीं होता, बल्कि उसके सोचने के मापदंड और रुचि तथा स्वभाव विशुद्ध पश्चिमी ढंग ही का होता है। लेकिन अगर इस वर्ग के कुछ लोग किसी ज़रूरत से इस्लाम या इस्लामी सभ्यता को जानना भी चाहें तो उनके सामने एकमात्र स्रोत पश्चिमी लेखकों और प्राच्यविदों की किताबें होती हैं। अगर संयोगवश किसी पश्चिमी लेखक या प्राच्यविद् के क़लम से इस्लाम के पक्ष में कोई अच्छी बात निकल जाए तो यह वर्ग भी उस हद तक इस्लाम की आंशिक उपयोगिता को मान लेता है, वर्ना इस वर्ग की प्रबल बहुसंख्या की नज़र में शरीअत की हैसियत यूरोप के अज्ञानकाल की पवित्र रोमन एम्पायर की व्यवस्था और क़ानूनों से भिन्न नहीं है। यह बात बड़ी दिलचस्प होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी है कि इस वर्ग के बहुत-से लोग इस्लामी इतिहास के बड़े हिस्से के लिए मध्य युग और अज्ञानकाल की पश्चिमी और यूरोपीय शब्दावलियाँ ही प्रयोग करते हैं।
मुस्लिम जगत् में शासकों का सम्बन्ध उपनिवेशवाद के दौर के आरम्भ से आम तौर से इसी वर्ग से रहा है। इसलिए शरीअत के बारे में इस वर्ग में सख़्त रिज़र्वेशन पाए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि एक अनलिखित समझौता इस बात का मौजूद है कि शरीअत को लागू करने, प्रचलित करने और पुनर्जीवित करने की कोशिशों को या तो दबा दिया जाए, और अगर दबाना सम्भव या निहितार्थों के अनुसार न हो तो उनको ज़्यादा-से-ज़्यादा सीमित रखने की कोशिश की जाए।
शरीअत के बारे में कुछ और ग़लत-फ़हमियाँ वे हैं जो क़ानूनविदों के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस वर्ग में मौजूद बहुत-से निष्ठावान और दीनदार (धार्मिक) लोग भी इन ग़लत-फ़हमियों से किसी-न-किसी हद तक प्रभावित नज़र आते हैं। ये ग़लत-फ़हमियाँ विशेष रूप से उन देशों के क़ानूनविदों में ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ अंग्रेज़ी या एँग्लो-सेक्सन क़ानून का वर्चस्व रहा है। इसकी वजह यह है कि जब विभिन्न मुस्लिम देशों उदाहरणार्थ जज़ाइर, मलाया, उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया, नाईजीरिया और दूसरे देशों में अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद के क़ब्ज़े का आरम्भ हुआ तो शुरू-शुरू में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सन्तुष्ट रखने की ख़ातिर उनसे यह वादा किया कि उनके मामलात शरीअत के अनुसार ही चलाए जाएँगे। चुनाँचे 1765 ई॰ के लगभग जब ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह-आलम द्वितीय के दरमियान दीवानी समझौता हुआ तो उसमें यह शर्त भी रखी गई थी कि मुसलमानों के मामलात शरीअत के अनुसार तय किए जाएँगे। इस वादे पर पूरे तौर पर अमल करने की नौबत तो कभी न आ सकी लेकिन मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलात बड़ी हद तक उनके अपने फ़िक़ही मसलक के अनुसार हल किए जाने लगे। इस उद्देश्य के लिए उपमहाद्वीप में फ़िक़्हे-हनफ़ी और फ़िक़्हे-जाफ़री की कुछ किताबें अंग्रेज़ी में अनुवाद की गईं। (याद रहे कि उनमें कुछ अनुवाद अधूरे भी हैं और ग़लतियों से भरे भी) इन अनुवादों के साथ-साथ कुछ मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम वकीलों ने पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कीं जिनका मूलस्रोत ये अधूरे अनुवाद भी थे और अंग्रेज़ी अदालतों की मिसालें भी। अदालती मिसालों पर आधारित यह भंडार क़ानूनविदों के वर्ग में शरीअत के नाम से याद किया जाता था। दो सौ साल की इस परम्परा ने शरीअत की शब्दावली को कुछ पारिवारिक मामलों की इस धारणा तक सीमित कर दिया है जो अंग्रेज़ी अदालतों के उदाहरणों के ज़रिये उभरता है, वे उदाहरण जिनका आरम्भ कुछ सीमित फ़िक़ही किताबों के अधूरे और ग़लत अनुवादों से हुआ था। यही वजह है कि जब इस वर्ग के किसी व्यक्ति के सामने शरीअत का नाम लिया जाता है तो उसके ज़ेहन में एक बहुत सीमित, अपूर्ण तथा प्राचीन कल्पना उभरती है जिसका आधुनिक काल में कोई अधिक महत्त्व नहीं होना चाहिए। शरीअत के बारे में ग़लत-फ़हमियाँ पैदा करने और उसकी सीमित परिकल्पना को जन्म देने में कुछ धार्मिक वर्गों का हिस्सा भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा। सूफ़ियों के हलक़े में तो एक लम्बे समय से ‘शरीअत’ को ‘तरीक़त’ और ‘हक़ीक़त’ के मुक़ाबले में एक कमतर दर्जे की चीज़ समझा जाता रहा है। विशेष रूप से स्वच्छन्दतावादी फ़ारसी शाइरों ने शरीअत और शरीअत की शब्दावलियों के साथ उपहासपूर्ण रवैया लम्बे समय से अपना रखा है। सम्भव है किसी निष्ठावान और आन्तरिक सुधार के पक्षधर किसी सूफ़ी को कुछ विद्वानों की ज़ाहिर-परस्ती से शिकायतें हुई हों और उनका इज़हार नकारात्मक टिप्पणियों के रूप में हुआ हो जिसकी कुछ मिसालें मौलाना रूम, हकीम सिनाई और ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार वग़ैरा के कलाम में मिलती हैं, लेकिन जिस कसरत और ज़ोर-शोर से फ़ारसी के बाद के शाइरों ने, और फिर उनके अन्धानुकरण में उर्दू के शाइरों ने शरीअत, क़ाज़ी, मुहतसिब, फ़कीह, शैख़, मदरसा, मस्जिद, काबा और ऐसी ही बहुत-सी शब्दावलियों को जो नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त किया, उसने स्वच्छन्दतावादी ज़ेहनों को और अधिक विषैला करने में अत्यन्त नकारात्मक भूमिका निभाई है।
हमारे यहाँ उपमहाद्वीप में पिछले सौ-सवा-सौ वर्षों के दौरान शरीअत से मुराद एक ख़ास सीमित धार्मिक वर्ग के तौर-तरीक़े लिए जाने लगे। चुनाँचे शरई पाजामा, शरई टोपी, शरई रूमाल और शरई बाल जैसी शब्दावलियाँ आपने बहुत सुनी होंगी। इन हालात में अगर शरीअत की शब्दावली को ग़लत समझा गया हो, उसके बारे में सीमित धारणाएँ ज़ेहनों में पाई जाती हों, एक वर्ग शरीअत के बारे में नकारात्मक सोच रखता हो, कुछ लोग शरीअत को मध्य युग की एक रूढ़िवादी व्यवस्था समझते हों तो इसमें दोष किसका है? इन हालात में इस बात की बहुत ज़रूरत है कि शरीअत के मूल अर्थों को आम किया जाए, शरीअत के व्यापक इस्लामी और अरबी अर्थ को स्पष्ट किया जाए और यह बताया जाए कि शरीअत क्या है, उसके कार्यक्षेत्र में क्या-क्या गतिविधियाँ शामिल हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका सम्बन्ध किस प्रकार का है, शरीअत की मौलिक धारणाएँ, आदेश और उद्देश्य क्या हैं, शरीअत के विशेष गुण क्या हैं। इसके अलावा आधुनिक काल के बौद्धिकतावादी और पश्चिमवादी ज़ेहनों को सन्तुष्ट करने के लिए यह बताना भी ज़रूरी है कि शरीअत की तत्वदर्शिता और दर्शन क्या है और परिवर्तन और दृढ़ता के इस निरन्तर संघर्ष में शरीअत क्या कहती है।
यह बात पहले क़दम के तौर पर ज़ेहन में रखनी चाहिए कि शरीअत मात्र किसी क़ानूनी व्यवस्था, या मात्र किसी संहिता या फ़ौजदारी क़ानून का नाम नहीं, बल्कि शरीअत से मुराद एक जीवन-शैली है, जिसका आधार और मूल सिद्धान्त अल्लाह की वह्य (ईश-प्रकाशना) पर ईमान और अल्लाह के अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाओं की पैरवी है। यह एक ऐसी जीवन-प्रणाली है जिसमें नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है।
शरीअत एक पैराडायम है जो विशिष्ट मानसिक रवैये का गठन करता है, वह मानसिक रवैया जिससे एक नई संस्कृति उभरती है, एक नई सभ्यता जन्म लेती है। एक ऐसी सभ्यता अस्तित्व में आती है जो रंग-नस्ल के भेदभावों और भाषायी तथा भौगोलिक पक्षपातों से परे है, जो इंसानों को अक़ीदा, नज़रिया और जीवन-शैली के आधार पर एकट्ठा करती है।
अरबी भाषा में शरीअत से अभिप्रेत वह स्पष्ट और चौड़ा रास्ता है जो इंसानों को पानी के मूल स्रोत तक पहुँचा दे। प्राचीन अरबी शाइरों ने ‘शरीआ’ और ‘शराए’ का शब्द उन रास्तों के लिए प्रयोग किया है जिनपर चलकर इंसान पानी के भंडार तक पहुँच सके। वह बस्ती या वह जगह जहाँ से पानी लाने और ले जाने के रास्ते बहुत आसान और चौड़े हों, उसके लिए ‘सहलुश्शराइअ’ का मिश्रण अरबी भाषा एवं साहित्य में प्रयुक्त होता है। चूँकि पवित्र क़ुरआन के अनुसार पानी ज़िन्दगी का मूल स्रोत है इसलिए हम कह सकते हैं कि शरीअत से मुराद वह रास्ता है जो इंसानों को भौतिक जीवन के मूल स्रोत तक पहुँचा दे।
पवित्र क़ुरआन के अनुसार वास्तविक और शाश्वत आख़िरत का जीवन है। चुनाँचे पवित्र क़ुरआन में कहा गया है— “आख़िरत (परलोक) का जीवन ही वस्तुतः वास्तविक जीवन है।” (क़ुरआन, 29:64) अत: वह रास्ता, वह सत्यमार्ग जिसपर चलकर इंसान वास्तविक जीवन तक पहुँच सके उसके लिए भी शरीअत की शब्दावली अपनाई गई।
पवित्र क़ुरआन और हदीसों से पता चलता है कि अल्लाह तआला ने अतीत में विभिन्न क़ौमों को शरीअत के विभिन्न आदेश प्रदान किए। इन शरीअतों का आधार एक ही था, लेकिन उनके व्यावहारिक विवरण स्थानीय आवश्यकताओं और समय की माँगों के अनुसार अलग-अलग थे। जिस क़ौम को जिस तरह की शिक्षा और क़ानूनों की ज़्यादा ज़रूरत थी उसको उसी प्रकार के क़ानून और आदेश दिए गए। चूँकि इन आदेशों के व्यावहारिक विवरणों में स्थानीय परिस्थितियों और समय का ध्यान रखते हुए कुछ ख़ास-ख़ास पहलुओं पर ज़ोर दिया गया था, इसलिए आदेशों और क़ानूनों के इन संग्रहों को विभिन्न शरीअतों के नाम से याद किया गया। चुनाँचे इस्लामी साहित्य में शरीअते-मूसवी और शरीअते-ईसवी का उल्लेख बहुत अधिक मिलता है। ख़ुद पवित्र क़ुरआन में विभिन्न समुदायों का उल्लेख करने के बाद उनको सम्बोधित करते हुए फ़रमाया गया— “हमने तुम सबके लिए एक-एक शरीअत और एक रास्ता बनाया है।” (क़ुरआन, 5:48)
अगरचे ये शरीअतें और इनपर कार्यान्वयन के ढंग और स्रोत विभिन्न रहे हैं लेकिन इन सबका आधार दीन के शाश्वत सिद्धान्तों पर रहा है। उपमहाद्वीप के सबसे बड़े इस्लामी चिन्तक और दक्षिण एशिया के मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘हुज्जतिल्लाहिल-बालिग़ा’ में बहुत विस्तार से इस बात को स्पष्ट किया है कि तमाम आसमानी किताबों में दीन के मौलिक सिद्धान्त एक ही रहे हैं और तमाम पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) ने उन्हीं की शिक्षा दी है। शाह वलीउल्लाह (रह॰) ने इस्लाम के सर्वसम्मत सिद्धान्तों की निशानदेही करते हुए निम्नलिखित अक़ीदों और धारणाओं का उल्लेख किया है—
- तौहीद (अल्लाह के एक होने) पर ईमान
- जो मामले अल्लाह तआला के अस्तित्व के बारे में उसके गौरवानुकूल नहीं उनसे उसको पाक समझना
- शिर्क को समाप्त करना
- नास्तिकता और धार्मिक विमुखता का उन्मूलन
- तक़दीर (अल्लाह की सामर्थ्य) पर पूरा यक़ीन
- अल्लाह की निशानियों का सम्मान
- फ़रिश्तों पर ईमान
- आसमानी किताबों पर ईमान
- क़ियामत पर ईमान
- जन्नत-दोज़ख़ (स्वर्ग-नरक) और आख़िरत (परलोक) के हिसाब पर ईमान
- आमाले-सालेहा (सत्कर्मों) यानी ‘बिर्र’ की क़िस्में
- आमाले-बद (दुष्कर्मों) यानी गुनाहों की क़िस्में
- अदलो-इंसाफ़ (न्याय) की स्थापना
- ज़ुल्मो-ज़्यादती की तमाम शक्लों की मनाही
- अल्लाह की हदों (सीमाओं और सज़ाओं) की स्थापना
- अल्लाह के रास्ते में जिहाद (संघर्ष)
- उत्तम नैतिकता को बढ़ावा देना
- नैतिक बुराइयों को समाप्त करना
इन तमाम मौलिक धारणाओं की शिक्षा तमाम पैग़म्बरों ने दी। अलबत्ता उनके व्यावहारिक विवरणों में मतभेद रहा है। प्राचीन शरीअतों में इन मामलों से सम्बन्धित व्यावहारिक आदेश सीधे-साधे और आरम्भिक प्रकार के थे। फिर ज्यों-ज्यों इंसानियत मानसिक रूप से विकसित होती गई इन आदेशों के विवरणों में वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि वह मरहला आ पहुँचा जब इंसानियत शरीअत के पूर्ण होने के लिए तैयार थी और ज़मीन का उपजाऊपन इस स्तर तक पहुँच चुका था कि अब इसमें अन्तिम, पूर्ण, विश्वव्यापी और बहुआयामी शरीअत का बीज बोया जाए।
शरीअते-मुहम्मदी या शरीअते-इस्लामी से मुराद वह समष्टीय शिक्षा है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़रिये इंसानों तक पहुँची। यह शिक्षा अल्लाह की वह्य (ईश-प्रकाशना) के द्वारा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक और उनके द्वारा इंसानों तक पहुँची। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक जो वह्य पहुँची है उसके दो प्रकार हैं। एक ‘वह्ये-जली’ कहलाती है जिसके शब्द और अर्थ दोनों अल्लाह तआला की ओर से भेजे गए। यह वह्य पवित्र क़ुरआन के रूप में सुरक्षित है। वह्य का दूसरा प्रकार ‘वह्ये-ख़फ़ी’ कहलाता है। इसके अर्थ और मतलब तो अल्लाह की तरफ़ से हैं, लेकिन इसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपनी मुबारक ज़बान से अपने शब्दों में या अपने व्यवहार से बयान किया। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के प्रदान किए हुए व्यवहार और मार्गदर्शन के लिए ‘सुन्नत’ की शब्दावली प्रयोग की जाती है। अरबी ज़बान में ‘सुन्नत’ का अर्थ व्यवहार और निर्धारित कार्य-प्रणाली है। यह शब्द इस्लाम से पहले भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता था। अरबी भाषा के प्रसिद्ध शाइर लबीद-बिन-रबीआ अल-आमिरी ने अपने प्रसिद्ध शेअर में ‘सुन्नत’ शब्द का प्रयोग किया है।
अरबी भाषा का यह शब्द अपने अर्थ की विशालता और व्यापकता की वजह से इतना उपयुक्त था कि इसी को अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुन्नत यानी व्यवहार और उसवए-हसना (उत्तम आदर्श) के लिए अपना लिया गया। शरीअत के इन दोनों स्रोतों यानी पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल के द्वारा जो शिक्षा यानी शरीअत हम तक पहुँची है उसके बड़े-बड़े और महत्त्वपूर्ण हिस्से तीन हैं—
1. अक़ीदा और ईमानियात
2. तज़किया, एहसान और नैतिकता
3. फ़िक़्ह यानी ज़ाहिरी आदेशों का संग्रह
इन लेक्चर्स में शरीअत के इन्हीं तीन पहलुओं का स्पष्टीकरण और व्याख्या अभीष्ट है। इनमें से पहले दो अंग निस्सन्देह मौलिक महत्त्व रखते हैं, लेकिन ज़रा ग़ौर करके देखा जाए तो वे एक दृष्टि से इस तीसरे और आख़िरी अंग के लिए भूमिका की हैसियत रखते हैं। शरीअत एक जीवन व्यवस्था है, एक जीवन-प्रणाली है, दुनिया में रहने का एक ख़ास ढंग है। इन सब पहलुओं का सम्बन्ध प्रायः इंसान की ज़ाहिरी ज़िन्दगी से ही होता है, अक़ीदा इंसान को मानसिक और वैचारिक दृष्टि से इस बात पर सन्तुष्ट करता है कि इस ज़िन्दगी में उसकी हैसियत और स्थान क्या है? उसका आरम्भ और अन्त क्या है? वह कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है? उसके चारों ओर फैली हुई इस दुनिया से उसके सम्बन्ध का प्रकार क्या है? इन सब सवालों के आरम्भिक और सैद्धान्तिक उत्तर ही को ‘अक़ीदा’ और ‘ईमानियात’ कहा जाता है। अक़ीदा और ईमानियात न हों तो इंसान ज़िन्दगी की कोई व्यवस्था नहीं बना सकता, इस धरती पर रहने-सहने का कोई ढंग या सलीक़ा नहीं बना सकता, दूसरों से मिल-जुलकर रहने का कोई नियम तय नहीं कर सकता। इनमें से हर चीज़ के लिए इन मौलिक प्रश्नों का कोई न कोई उत्तर तय करना ज़रूरी है। इससे पता चला कि अक़ीदा और ईमानियात ही वास्तव में वे बुनियादें हैं जिनपर कर्म की इमारत खड़ी होती है। यही कैफ़ियत ‘तज़किया’ और ‘एहसान’ और ‘अख़्लाक़ियात’ (नैतिकता) की है। तज़किया और एहसान से मुराद इंसान का आन्तरिक प्रशिक्षण और आन्तिरक सुधार है। जिस उच्च नैतिकता की शरीअत ने शिक्षा दी है अगर वह इंसान की नस-नस में रची बसी न हों तो प्रतिदिन जीवन में उनपर निस्संकोच अमल करना आसान नहीं। तज़किया और एहसान की हैसियत इमारत के मौलिक स्तम्भों और दीवारों की है। ये न हों तो अव्वल तो इमारत बन नहीं सकती, और किसी-न-किसी तरह बन भी जाए तो क़ायम नहीं रह सकती। इन दोनों महत्त्वपूर्ण और आधारभूत अंगों के बाद तीसरा, सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे विस्तृत मैदान ज़ाहिरी कर्मों और ज़ाहिरी ज़िन्दगी के मार्गदर्शन का है जिसपर अमल करने के लिए इंसानों को तैयार करने और आमादा रखने का काम अक़ीदा और ईमानियात और तज़किया और एहसान की शिक्षा के द्वारा होता है। चूँकि फ़िक़्ह का कार्यक्षेत्र पूरे मानव जीवन पर प्रभावी है इसलिए उसको शरीअत का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू और सबसे मौलिक अंग समझना ग़लत नहीं है। इतना महत्त्वपूर्ण और मौलिक कि कभी-कभी फ़िक़्ह को ही शरीअत कह दिया जाता है। यह शैली न केवल अरबी भाषा, बल्कि दुनिया की और भी कई भाषाओं और समाजों में आम है कि किसी चीज़ के सबसे महत्त्वपूर्ण या बहुत महत्त्वपूर्ण अंगों को पूर्णता मान लिया जाता है। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाक़ों को आज भी उपमहाद्वीप के बहुत-से इलाक़ों में हिन्दुस्तान कहा जाता है। मिस्र में क़ाहिरा के लिए मिस्र और शाम (सीरिया) में दमिशक़ के लिए शाम के शब्द आज भी सुनने में आते हैं।
इससे पहले कि शरीअत के कुछ मौलिक सिद्धान्तों और महत्त्वपूर्ण पहलुओं की बात शुरू की जाए उचित मालूम होता है कि पहले शरीअत की कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण और मौलिक विशिष्टताओं पर एक नज़र डाल ली जाए जो ख़ुद शरीअत की वास्तविकता को समझने के लिए ज़रूरी हैं। ये शरीअत की वे विशिष्टताएँ हैं जिनको जाने बिना ख़ुद शरीअत को पूरे तौर पर जानना मुश्किल है। शरीअत की अन्य विशिष्टताओं पर आगे चर्चाओं में बात होगी।
शरीअत की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी व्यापकता और विशालता है। यह बात हम पहले कह चुके हैं कि शरीअत अल्लाह द्वारा प्रदान की हुई वह आख़िरी जीवन व्यवस्था है जो अल्लाह के आख़िरी पैग़ंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के द्वारा अवतरित की गई। इसका मूलस्रोत वह आख़िरी ईशग्रन्थ है जो तमाम आसमानी किताबों के बाद अवतरित किया गया। पवित्र क़ुरआन के अपने शब्दों में वह जहाँ पिछली किताबों की पुष्टि करती है वहीं वह तमाम पिछली किताबों की निगराँ, उनकी रक्षक और उनके विषयों पर हावी है। निगराँ (मुहैमिन) के इस गुण से जहाँ पवित्र क़ुरआन की व्यापकता और परिपूर्णता का पता चलता है वहीं पवित्र क़ुरआन की दी हुई शरीअत की व्यापकता का भी अन्दाज़ा होता है।
शरीअत की व्यापकता पर चर्चा करने के कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू शरीअत की व्यापकता का वे विषय और वार्ताएँ हैं जिनसे शरीअत में बहस की गई है और जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए हैं। इन बातों से अन्दाज़ा होता है कि इस्लामी शरीअत ने ज़िन्दगी के तमाम महत्त्वपूर्ण पहलुओं के बारे में निर्देश दी हैं और उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है। जीवन के हर पहलू में कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ मानव बुद्धि या तो ग़लती कर सकती हो, या वहाँ ग़लती की सम्भावना पाई जाती हो, अतीत में बुद्धि इन मामलों में गलतियाँ करती रही हो, या उसका सम्बन्ध किसी ऐसे मामले से हो जो मानव बुद्धि की पहुँच से परे हो। ऐसे तमाम मामलों में शरीअत ने मौलिक निर्देश दिए हैं और उन मौलिक निर्देशों की रौशनी में मानव बुद्धि को आज़ाद छोड़ दिया है कि मानव बुद्धि शेष विवरण और शेष आंशिक सवालों के जवाब इन आम और सैद्धान्तिक उत्तरों की रौशनी में ख़ुद ही तय कर ले।
हम कह सकते हैं कि ये मौलिक प्रश्न जिनका पवित्र क़ुरआन ने उत्तर दिया है जिनका और अधिक विस्तृत विवरण सुन्नते-रसूल में बयान हुआ है, जिनका सम्बन्ध अक़ीदों से भी है, जिनका सम्बन्ध इंसान के रवैये, व्यवहार और भावनाओं से भी है, जिनका सम्बन्ध इंसान की अनुभूतियों और आन्तरिक प्रवृत्तियों से भी है, जो इंसान की नैतिकता और चरित्र से भी बहस करती हैं और उन सब चीज़ों से बढ़कर मानव जीवन के असीमित ज़ाहिरी पहलुओं पर भी मार्गदर्शन करती और निर्देश देती हैं, यह इंसानी कंप्यूटर को मौलिक कार्यकुशलता उपलब्ध करनेवाला सॉफ़्टवेअर (soft ware) है। जिस तरह एक जटिल-से-जटिल और उत्कृष्टतम मशीनी कंप्यूटर को एक सॉफ़्टवेअर की ज़रूरत होती है उसी तरह अल्लाह द्वारा रचित यह शाहकार (उत्कृष्ट कृति) कंप्यूटर भी एक सॉफ़्टवेअर का मुहताज है। इस सॉफ़्टवेअर से काम लेकर यह कंप्यूटर वे तमाम काम कर सकता है जो इंसानों को ज़िन्दगी में करने हैं। इस दृष्टि से शरीअत की व्यापकता का यह अर्थ नहीं है कि शरीअत ने मानव बुद्धि के सोचने-समझने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, या मानव बुद्धि की भूमिका को सीमित कर दिया है, या मानव बुद्धि की कार्यकुशलता शरीअत की रौशनी में असन्तोषजनक या अस्वीकार्य है। इसका अर्थ केवल यह है कि मानव बुद्धि की ज़िम्मेदारी शरीअत के दिए हुए निर्देशों की पूर्ति और उससे सम्बन्धित उन विस्तृत विवरणों की निशानदेही है जिनको बयान करना पवित्र क़ुरआन या सुन्नते-रसूल ने इंसान की सद्बुद्धि और सही समझ पर भरोसा करते हुए ज़रूरी नहीं समझा।
दूसरी ओर शरीअत की व्यापकता का एक पहलू उसकी व्यापकता और परिपूर्णता भी है। व्यापकता से मुराद यह है कि दूसरी आसमानी किताबों, दुनिया के क़ानूनों, सभ्यता के सिद्धान्तों, सामाजिक तरीक़ों और सांस्कृतिक रवैयों के विपरीत जो किसी-न-किसी दृष्टि से सीमित पहलुओं से बहस करते हैं शरीअत की दिलचस्पी का दायरा बहुत विस्तृत है। अगर यह कहा जाए तो ग़लत न होगा कि इन तमाम व्यवस्थाओं, धारणाओं और विचारधाराओं के मुक़ाबले में शरीअत की दिलचस्पी का दायरा सबसे विशाल है। इस विशालता का एक उदाहरण शरीअत की वह परिपूर्णता भी है जिसकी ओर कुछ हदीसों में इशारे किए गए हैं। मिसाल के तौर पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “मुझे केवल इस उद्देश्य के लिए भेजा गया है कि मैं उच्च नैतिकता को पूर्ण करूँ।” उच्च नैतिकता की परिपूर्णता से अभिप्रेत यह है कि इंसानों में पहले से मौजूद उच्च नैतिकता को न केवल बरक़रार रखा जाए, बल्कि नैतिकता की तमाम बिखरी और आंशिक धारणाओं को सहेजकर इकट्ठा कर दिया जाए और नैतिकता की एक सारगर्भित और पूर्ण परिकल्पना इंसानों को दे दी जाए। यह बात स्पष्ट है कि उच्च नैतिकता सभी मानव सभ्यताओं में पहले से मौजूद थी, उच्च नैतिकता की मौलिक धारणाएँ पहले से इंसानों को दी जा चुकी थीं, उच्च नैतिकता के बहुत-से पहलुओं पर इंसान पहले से अमल कर रहे थे, लेकिन यह उच्च नैतिकता अलग-अलग रूप में अलग-अलग क़ौमों को दी गई थी। जिन-जिन क़ौमों को जिन नैतिक निर्देशों की ज़्यादा ज़रूरत थी उन नैतिक निर्देशों पर उनके पैग़म्बरों ने ज़ोर दिया था। और विशेष रूप से उन नैतिक कमज़ोरियों को दूर करने से दिलचस्पी ली थी जो उनकी विशिष्ट क़ौमें या उनके विशिष्ट इलाक़ों में पाई जाती थीं। लेकिन अब चूँकि एक ऐसी नैतिक व्यवस्था और मार्गदर्शन व्यवस्था देने का मरहला आ चुका था जो सभी इंसानों के लिए, सभी इलाक़ों के लिए और सभी कालों के लिए हो इसलिए अब इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि उन तमाम नैतिक धारणाओं, नैतिक प्रवृत्तियों और अतीत में दिए गए तमाम नैतिक दर्शनों को एक लड़ी में पिरो दिया जाए, एक व्यापक लड़ी में पिरोकर उनकी सुन्दर माला बना दी जाए। ये बिखरे हुए फूल जो विभिन्न क़ौमों में थे, ये विभिन्न मोती जो विभिन्न समयों और ज़मानों और विभिन्न स्थानों पर लोगों को दिए गए, विभिन्न जौहरियों ने अपनी क़ौम को प्रदान किए थे, अब ज़रूरत इस बात की थी कि इन तमाम फूलों को इकट्ठा करके एक व्यापक गुलदस्ता बनाया जाए, इन सभी मोतियों को इकट्ठा करके साफ़-सुथरा किया जाए, ज़माने की गर्दो-ग़ुबार से उनको धोया जाए, ज़माने की ग़लत-फ़हमियों के धब्बे ख़त्म किए जाएँ और उनको एक लड़ी में पिरोकर एक सुन्दर आभूषण का रूप दे दिया जाए। यह अर्थ है उच्च नैतिकता की परिपूर्णता का।
यहाँ यह बात याद दिलाना भी उचित होगा कि जब मुतकल्लिमीने-इस्लाम, इस्लामी फ़ुक़हा या इस्लामी विद्वानों ने इस्लाम की तमाम शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग ज्ञान के रूप में संकलित किया तो उन्होंने विभिन्न क़ौमों से आनेवाली बहुत-सी तत्त्वदर्शितापूर्ण बातों को इस्लाम की व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया। चुनाँचे जो दार्शनिक और मुतकल्लिमीन नैतिक ज्ञान को संकलित कर रहे थे उन्होंने नैतिक दृष्टि से जहाँ-जहाँ जिस क़ौम में जो ख़ूबी महसूस की उस ख़ूबी को इस्लाम की नैतिकता की धारणा या नैतिक दर्शन की पूर्ति और स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया। इसलिए इस्लामी सोच और इस्लामी फ़िक्र में कुछ आंशिक समानताएँ विभिन्न क़ौमों सी पाई जाती हैं। कुछ ज़ाहिर में उन आंशिक समानताओं को देखकर इस्लामी विचारधारा की मौलिकता यानी (Originality) का इनकार करने लगते हैं और वे यह समझते हैं कि मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने या इस्लामी फ़ुक़हा ने जो कुछ संकलित किया है वह सब दूसरों से लिया हुआ है। हालाँकि दूसरों के पास अगर तत्त्वदर्शिता के कोई मोती हैं तो उनको एक व्यापक लड़ी में पिरोना भी इस्लाम के मौलिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आगमन का उद्देश्य ही उच्च नैतिकता की पूर्ति बताया गया, उच्च नैतिकता की ईजाद नहीं बताया गया। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह नहीं फ़रमाया कि मैं कोई नई नैतिक व्यवस्था लेकर आया हूँ, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तो फ़रमाया, “मैं कोई नया रसूल नहीं हूँ, नया सन्देश लेकर नहीं आया। पूर्व सन्देशों की पूर्ति, नवीनीकरण और उन्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ।” इस पहलू से अगर पिछली क़ौमौं की धार्मिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और क़ानून विभाग पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि विभिन्न क़ौमों में पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षा के अवशेष जगह-जगह बिखरे हुए मौजूद थे। जिन इलाक़ों या जिन स्थानों के पैग़म्बरों का पवित्र क़ुरआन या हदीसों में उल्लेख नहीं है, इसलिए कि अरब उनसे परिचित नहीं थे, क़ुरआन ने सर्वप्रथम जिन्हें सम्बोधित किया उनके यहाँ वे नाम परिचित नहीं थे, इसलिए पवित्र क़ुरआन ने उनका नाम लेना उचित नहीं समझा, लेकिन नबी और रसूल हर क़ौम में आए, इसलिए हर क़ौम में पैग़म्बर की शिक्षाओं के कुछ-न-कुछ अवशेष मौजूद हैं। इन अवशेषों का सार और आत्मा पवित्र क़ुरआन में सुरक्षित है। व्यावहारिक रूप से जगह-जगह पिछले नबियों (अलैहिमुस्सलाम) की किताबों और सन्देशों के हवाले से कुछ मिसालें बयान की गई हैं। इन सबको अब एक व्यापकता का गौरव प्रदान करना परिपूर्णता के रंग में उनको रंग देना, और उन भिन्न-भिन्न फूलों का एक गुलदस्ता बना देना, बल्कि बिखरे हुए पौधों से एक बाग़ बना देना यह आख़िरी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का मौलिक काम था।
यह गौरव इबादतों में बड़ा नुमायाँ मालूम होता है। पवित्र क़ुरआन से पता चलता है कि दुनिया की हर क़ौम में, दुनिया की हर व्यवस्था में अल्लाह की इबादत के कुछ-न-कुछ तरीक़े प्रचलित और मौजूद थे। ख़ुद पवित्र क़ुरआन में कहा गया है, “हमने तुममें से हर एक के लिए अपने-अपने समय में एक शरीअत मुक़र्रर की थी और एक रास्ता तुम्हें प्रदान किया था।” शरीअत पर अमल करने के वे तरीक़े भी बताए थे, जो तुम्हारे हालात और ज़माने के लिहाज़ से थे और तुम उसपर अमल करते रहे। अल्लाह तआला की नियति इस मामले में यह नहीं थी कि तुम सबको एक मुस्लिम समुदाय बना देता, लेकिन उस समय तुम एक मुस्लिम समुदाय बन नहीं सकते थे। अल्लाह तआला की क्रम से कार्य करने की नीति के ख़िलाफ़ था कि पहले दिन से, इंसानियत के आरम्भ से ही, सारी इंसानियत को एक अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्मानवीय समुदाय बना दिया जाता। यह सम्भव नहीं था, इंसान इसके लिए तैयार नहीं था, इंसानों के प्रशिक्षण के चरण इस दर्जे तक नहीं पहुँचे थे कि उनको एक विश्वव्यापी और अन्तर्मानवीय समुदाय की लड़ी में पिरो दिया जाता। लेकिन जब यह समय आ गया उस समय यह काम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुबारक हाथों से हुआ और पवित्र क़ुरआन ने एक-एक करके उन तमाम शिक्षाओं को पूर्ण कर दिया जिनके विभिन्न पहलू और विभिन्न अंग विभिन्न पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) लेकर आए थे। उनमें से बहुत-से हिस्से अभी आने बाक़ी थे जिनके लिए इंसानियत मानसिक, वैचारिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं थी। परिपूर्णता का यह गौरव इबादतों में सबसे नुमायाँ मालूम होता है। नमाज़ की इबादत को अगर देखा जाए तो नमाज़ की तरह की कोई-न-कोई इबादत दुनिया की हर क़ौम में पाई जाती है। दुनिया की हर क़ौम में अल्लाह की इबादत की परिकल्पना मौजूद है। इबादतों में सबसे नुमायाँ इबादत शारीरिक इबादत है जिसमें इंसान अपने जिस्म की हरकतों से, अपने उठने-बैठने से और विनम्रता के प्रदर्शन से इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि वह अल्लाह का पैरोकार है, अल्लाह के आदेश के अधीन है, अल्लाह के सामने सिर झुकाने और उसके आदेशों के अनुसार सजदा करने के लिए तैयार है। वह अपने माथे को ज़मीन पर रखने के लिए हर समय तैयार है। यह रूह अल्लाह के हर पैग़ंबर ने इंसानों के अन्दर स्थानान्तरित करने की कोशिश की। विभिन्न पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) ने जो नमाज़ सिखाई थी या जिस जिस्मानी इबादत की शिक्षा दी थी उसका वास्तविक रूप क्या था उसका विवरण हमें मालूम नहीं है, इसलिए कि पवित्र क़ुरआन ने उसको बयान नहीं किया, पिछले पैग़म्बरों की किताबें अपने मूल रूप में आज मौजूद नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल है कि उदाहरणार्थ हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) किस तरह की इबादत करते थे, हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम को किस तरह की नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया था, हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) किस तरह अल्लाह की इबादत का फ़र्ज़ अंजाम दिया करते थे। अलबत्ता आज विभिन्न क़ौमों में नमाज़ों के या इबादतों के जो तरीक़े प्रचलित हैं उनको देखकर अन्दाज़ा होता है कि कुछ क़ौमों में सिर्फ़ क़ियाम ही का नाम नमाज़ या इबादत है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की कुछ क़ौमों में इबादतगाह में जाकर ख़ामोश खड़े हो जाना और कुछ देर ख़ामोश खड़े रहना इबादत समझा जाता है। वह बुतों के सामने हो या जिस चीज़ को वह क़िबला समझते हैं, उसके सामने हो या जिस चीज़ को वह अल्लाह की निशानी समझते हैं उसके सामने हो, लेकिन ख़ामोश खड़ा रहना इबादत के एक रूप के तौर पर आज भी कुछ क़ौमों में प्रचलित है। पवित्र क़ुरआन में इसका इशारा मिलता है, “अल्लाह के सामने ख़ामोश खड़े हो जाओ।” गोया क़ियाम को नमाज़ का एक अंग बना दिया गया और यह क़ियाम नमाज़ की क्रियाओं में से है। कुछ और क़ौमों के यहाँ एक ऐसी इबादत प्रचलित है, जिसको हम रुकू के समान कह सकते हैं। चुनाँचे अंग्रेज़ी भाषा में (Kneeling down) का मुहावरा आज भी कुछ क़ौमों में प्रयुक्त होता है। उनकी इबादतगाहों और गिरजाघरों में ख़ास अन्दाज़ की कुर्सियाँ बनाई गई हैं जिसमें लोगों को रुकू करने में या (Kneel down) करने में आसानी हो जाती है। इससे पता चला कि रुकू यानी अल्लाह के सामने झुक जाना और अल्लाह के सामने इन्तिहाई तुच्छता के साथ यानी इंसान अपने मन और अपने स्वभाव को अल्लाह के सामने पूरे तौर पर झुका दे और जिस्मानी तौर पर भी इसका इज़हार करे। यह चीज़ रुकू से ज़ाहिर होती है। कुछ क़ौमों में सजदे की परम्पराएँ भी मौजूद हैं अगरचे कम हैं। जिस अन्दाज़ का सजदा मुसलमान करते हैं इस अन्दाज़ का सजदा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन किसी-न-किसी अन्दाज़ में पाया जाता है। कुछ और क़ौमों में खड़े होकर दुआ करने की धारणा है, जिसके लिए इस्लामी शब्दावली ‘क़ुनूत’ है। कुछ और क़ौमों में अल्लाह से प्रार्थना करना अल्लाह के सामने दुआएँ पढ़ना, धार्मिक श्लोकों का पाठ करना, अल्लाह के सामने नज़्में पढ़ना, यह सब भी इबादत का एक हिस्सा समझा जाता है। कुछ क़ौमों में ख़ामोश बैठ जाना इबादत समझा जाता है। यह वह चीज़ है जिसको इस्लामी शब्दावली में ‘क़ादा’ कहते हैं। इससे अन्दाज़ा हुआ कि आज भी दुनिया के विभिन्न धर्मों में और दुनिया की विभिन्न क़ौमों में इबादतों के जो अंग पाए जाते हैं जिनके बारे में हम पवित्र क़ुरआन के कथनों की रौशनी में कह सकते हैं कि ये सब अंग पिछले नबियों (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षा के अवशेष मालूम होते हैं। इन सबको पवित्र क़ुरआन में विभिन्न स्थानों पर बयान किया गया है, और नमाज़ की इबादत में इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। इसके अलावा इस्लाम का स्वभाव जाननेवालों ने, विशेष रूप से तसव्वुफ़ के समर्थकों ने, यह लिखा है कि पवित्र क़ुरआन में जो आया है कि “हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है” और एक जगह आया है कि “अल्लाह की हर मख़्लूक़ अल्लाह के सामने सजदा कर रही है।” कुछ मख़्लूक़ात (स्रष्ट रचनाएँ) हैं जो मजबूरन अल्लाह के सामने नतमस्तक हैं जिनको अल्लाह ने पैदा ही इस तरह किया है कि वे सदा नतमस्तक ही रहें, और कुछ मख़्लूक़ात हैं जो स्वेच्छापूर्वक अल्लाह के सामने नतमस्तक रहती हैं जैसे इंसान, फ़रिश्ते और जिन्नात।
वे मख़्लूक़ात जो अनैच्छिक रूप से अल्लाह के आदेशों का पालन करती हैं उनमें से कुछ स्थायी रूप से ‘क़ियाम’ की हालत में हैं, कुछ स्थायी रूप से ‘रुकू’ की हालत में हैं, कुछ स्थायी रूप से सजदे की हालत में हैं, कुछ स्थायी रूप से ‘क़ादा’ की हालत में हैं। ये वे ज़ाहिरी गतिविधियाँ हैं जो नमाज़ में की जाती है। अगर नमाज़ के सिर्फ़ ज़ाहिरी पहलुओं को लिया जाए तो यह ज़ाहिरी पहलू, जो चार बड़े-बड़े पहलू हैं, ये विभिन्न मख़्लूक़ात में मौजूद हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अल्लाह तआला की इबादत के जितने तरीक़े मख़्लूक़ात में प्रचलित हैं, वे तशरीई (वे आदेश जिनपर चलने-न-चलने के लिए इंसान आज़ाद है) तौर पर प्रचलित हुए हों या तकवीनी (वे प्राकृतिक स्वभाव जिसे अल्लाह ने बनाया है और जिससे कोई प्राणी मुँह नहीं मोड़ सकता) तौर पर प्रचलित हों। नमाज़ उन सबको इकट्ठा कर देती है और उन सबके सार की हैसियत रखती है।
नमाज़ के अरकान (क्रियाओं) के सिलसिले में एक बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है और वह नमाज़ का आख़िरी क़ादा है। जब नमाज़ का एक यूनिट या दो रकअतें पूरी होती हैं तो नमाज़ी क़ादे में बैठता है और क़ादे में बैठकर वह ‘अत्तह्हियातु लिल्लाहि...’ की तिलावत करता है। ‘अत्तह्हियातु लिल्लाहि वस-स-ल-वातु वत्तय्यिबातु’ की यह दुआ दरअस्ल वह संवाद है जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और अल्लाह तआला के दरमियान हुआ था। जब अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मेराज के मौक़े पर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे जहाँ कोई और मख़्लूक़ उनसे पहले नहीं पहुँच सकी, जहाँ दाख़िले से पहले जिब्रील अमीन तक ने आगे साथ जाने से खेद प्रकट कर दिया था।
हम कह सकते हैं कि नमाज़ का यह आख़िरी हिस्सा मेराज का (action replay) है। शायद यही वजह है कि नमाज़ के बारे में फ़रमाया गया कि “नमाज़ मुसलमानों की मेराज है।” अगर मुसलमान यह समझकर नमाज़ अदा करे कि वह आज तक की जानेवाली तमाम इबादतों की रूह अपने इस कर्त्तव्य के द्वारा अंजाम दे रहा है, सृष्टि की तमाम मख़्लूक़ात के इबादत के तरीक़े का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पिछले नबियों और पिछली शरीअतों ने जिस-जिस तरीक़े से अल्लाह की इबादत का ढंग सिखाया उन सब तरीक़ों को प्रयोग करके अल्लाह की इबादत कर रहा है और उसकी समाप्ति मेराज के इस आख़िरी प्वाइंट की चर्चा के दोहराने पर होगी तो फिर नमाज़ की तत्त्वदर्शिता और परिपूर्णता का एक निराला रंग सामने आएगा।
नमाज़ के अलावा ज़कात, हज और रोज़े में भी यही शान पाई जाती है। इनमें से हर इबादत का अगर इसी तरह जायज़ा लिया जाए तो अन्दाज़ा होगा कि उनमें भी पिछले पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षा के विभिन्न तत्त्व जगह-जगह समो दिए गए हैं। हज, जिसकी दावत सबसे पहले हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने दी और इसलिए दी कि वे पहले अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्मानवीय, बल्कि अन्तर्महाद्वीपीय सन्देश रखनेवाले पैग़ंबर थे। अन्तर्महाद्वीपीय इस तरह कि उनका जन्म इराक़ में हुआ, फिर युवावस्था फ़िलस्तीन में गुज़री फिर वे अरबद्वीप में आए, एक लम्बे समय के लिए मिस्र भी गए, कुछ और इतिहासकारों की राय के अनुसार वे यूरोप भी गए, भारत में भी आए और यों विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न इलाक़ों में उन्होंने अल्लाह के सन्देश का प्रचार-प्रसार किया।
चूँकि हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) पहले विश्वव्यापी और अन्तर्मानवीय सन्देश रखनेवाले नबी थे इसलिए उनके समुदाय का पवित्र क़ुरआन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मुसलमानों को उनकी ‘मिल्लत’ (समुदाय) का अनुयायी क़रार दिया गया। हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) को मुसलमानों का रूहानी बाप क़रार दिया गया और हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की शुरू की हुई इबादत यानी हज इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत क़रार दी गई और इस्लाम की अन्तर्मानवीयता का सबसे बड़ा प्रदर्शन हज को क़रार दिया गया। यही वजह है कि हज के मौक़े पर सबसे ज़्यादा जिस पैग़म्बर की सुन्नत और व्यवहार को याद किया जाता है वह हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। ‘क़ुर्बानी’ उनकी याद में होती है, ‘तवाफ़’ उनकी याद में होता है, सफ़ा और मर्वा के दरमियान ‘सई’ (दौड़) उनकी पत्नी और उनके बेटे की याद में होती है। हज की जितनी क्रियाएँ हैं उनमें हज़रत इबराहीम (अलैहिस्सलाम) की शिक्षा और सुन्नत की रूह इतनी रची-बसी है कि हज के पूरे सफ़र में इबरहीमियत की शान नुमायाँ तौर पर नज़र आती है।
ये मिसालें जिनमें और भी वृद्धि की जा सकती है, इस बात को बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि इस्लाम व्यापकता की शान भी रखता है और परिपूर्णता की शान भी। इस्लामी शरीअत दूसरी शरीअतों को समाप्त करनेवाली भी है दूसरी शरीअतों को इकट्ठा करनेवाली भी और उन्हें पूर्ण करनेवाली भी है। यह तमाम शरीअतों की पूर्णता के लिए भेजी गई।
व्यापकता और परिपूर्णता की एक अनिवार्य अपेक्षा यह भी है कि इस्लामी शरीअत एक वैश्विक या विश्वव्यापी शरीअत हो। यानी आलमियत और आलमगीरियत एक ऐसा गुण है जो व्यापकता और परिपूर्णता की अनिवार्य अपेक्षा है। इसी तरह आलमियत और आलमगीरियत की अनिवार्य अपेक्षा व्यापकता और परिपूर्णता है। ये दोनों गुण एक-दूसरे के लिए अनिवार्य हैं। अगर इस्लामी शरीअत को विश्वव्यापी शरीअत होना है तो उसको व्यापक शरीअत भी होना चाहिए, उसे पूर्ण करनेवाली शरीअत भी होनी चाहिए। अगर इस्लामी शरीअत दूसरी शरीअतों को जमा करनेवाली है और तमाम शरीअतों की पूर्ति करती है तो उसको विश्वव्यापी शरीअत भी होना चाहिए। इसलिए आलमगीरियत या आलमीयत इस्लामी शरीअत की दूसरी बड़ी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। यह शरीअत इंसानी विभाजनों, पक्षपातों से परे है। यह भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह इंसानों की नस्ली, भाषायी, रंग-आधारित, क्षेत्रीय विभाजनों को स्वीकार नहीं करती। इस दृष्टि से कि इन सब क़ौमों के लिए इस्लामी शरीअत अब एकमात्र जीवन व्यवस्था की हैसियत रखती है।
इन विभाजनों को स्वीकार न करने का यह अर्थ नहीं हैं कि इस्लाम इन तथ्यों के अस्तित्व ही को स्वीकार नहीं करता। लोगों की भाषाएँ विभिन्न होना तो एक वास्तविकता है। लोगों का विभिन्न इलाक़ों में रहना तो एक वास्तविकता है। लोगों का विभिन्न नस्लों से सम्बन्धित होना तो एक वास्तविकता है। इन तथ्यों का अर्थ सिर्फ़ यह है कि इस्लाम ने इन तमाम मतभेदों या विविधताओं को पहचान का ज़रिया क़रार दिया है, इंसानों के विभाजन का कारण नहीं ठहराया। इस्लाम इन विविधताओं के आधार पर इंसानों के अलगाव और विभाजन की अनुमति नहीं देता। मानव समानता और न्याय तथा इंसाफ़ की धारणाओं का इनकार करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन जहाँ तक इन भेदभावों का सम्बन्ध है इनका अस्तित्व एक वास्तविकता है। पवित्र क़ुरआन ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया है। इनके आधार पर लोगों की पहचान की जाती है। लोग अपना परिचय अपने इलाक़े से, अपने देश से, अपने वतन से, अपने क़बीले से, अपनी क़ौम से, अपनी बिरादरी से, अपनी भाषा से कराते हैं। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से प्रेम होना स्वाभाविक बात है। हर व्यक्ति अपने वतन से जहाँ उसका जन्म हुआ हो स्वाभाविक रूप से एक गहरा सम्बन्ध रखता है, जहाँ उसका बचपन गुज़रा हो, जहाँ उसके बाप-दादा पले बढ़े हों, उस इलाक़े और उस सरज़मीन से प्रेम होना एक स्वाभाविक बात है। इस्लाम इसको स्वीकार करता है। यह विविधता या यह फ़र्क़ इस्लाम सार्वभौम्य होने के ख़िलाफ़ नहीं है।
इस्लामी आलमियत (सार्वभौमिकता) से तात्पर्य यह है कि अब दुनिया की तमाम क़ौमों और दुनिया के तमाम इलाक़ों के लिए एक ही जीवन व्यवस्था होगी, एक ही शरीअत होगी जिसमें मौलिक धारणाएँ एक होंगी, उसूल और आरम्भिक सिद्धान्त साझे होंगे। आंशिक विवरण हर क़ौम, हर इलाक़ा और हर ज़माना अपने लिए अलग-अलग तय कर सकता है। आदेशों में हालात और ज़माने का ध्यान रखना यह शरीअत का स्वभाव है। यह इस्लाम की शरीअत की तत्त्वदर्शिता का एक अनिवार्य अंग और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है और इस्लामी सार्वभौमिकता की एक अनिवार्य अपेक्षा भी है।
इस्लामी शरीअत की तीसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी गहराई है। विशालता और व्यापकता की हम बात कर चुके हैं। विशालता के साथ शरीअत के आदेशों में गहराई भी पाई जाती है। गहराई से मुराद यह है कि इंसानों के मामलात के बारे में निर्देश देना, इंसानों के लिए नियम निर्धारित करना मात्र किसी सतही आधार पर नहीं है, जैसा कि दुनिया की बहुत सारी व्यवस्थाओं में पाया जाता है। शरीअत ने इंसान के स्वभाव, इंसान की मनोवृत्ति और इंसान की कमज़ोरियों और ख़ामियों को अच्छी तरह समझते हुए इंसान के लिए जीवन व्यवस्था निर्धारित की है। सृष्टि के रचयिता से ज़्यादा कौन इंसान की कमज़ोरियों और आवश्यकताओं को समझ सकता है। इसलिए शरीअत के आदेशों में इंसानी आवश्यकताओं का लिहाज़ रखा गया है। इंसानी आवश्यकताओं की विविधता असीमित है, इंसानी आवश्यकताएँ भी असीमित हैं। इंसान के स्वभाव की निशानियाँ अनगिनत हैं। इन सब विविधताओं का एक साथ ध्यान रखना और ऐसी जीवन व्यवस्था उपलब्ध करना जो तमाम इंसानों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, ऐसी व्यवस्था केवल सृष्टि का रचयिता ही दे सकता था। इंसानों के लिए यह सम्भव नहीं कि वह अपने लिए ऐसी व्यवस्था बना सकें। इसका कारण यह है जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा कि इंसान अपने ज़ेहन, अपनी नज़र, अपने अवलोकन, अपने अध्ययन और जानकारी की दृष्टि से अपने समय और जगह से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल महसूस करता है। बहुत थोड़े इंसान हैं जो अपने समज और स्थान से कुछ सौ साल पीछे या कुछ सौ साल आगे देख सकते हों। वर्ना इंसानों की बड़ी संख्या वह है जो अतीत से तो शायद परिचित हो, इसलिए कि संकलित इतिहास ने अतीत का ख़ासा हिस्सा सुरक्षित कर लिया है। लेकिन बहुत थोड़े इंसान हैं जो अपने हाल से कुछ साल आगे देख सकते हों। बड़े-बड़े चिन्तक कुछ सौ साल से आगे देखने में अक्षम रहते हैं। लेकिन यह बात कि मानवता कब तक धरती पर आबाद है, कितने हज़ार साल और इंसानों को ज़िन्दा रहना है, उन इंसानों की आवश्यकताएँ क्या होंगी, उनके मानसिक साँचे क्या होंगे, उनकी माँगें क्या होंगी, उनके दिमाग़ों में किस-किस तरह के सन्देह और सवालात पैदा होंगे, इंसानी ज़ेहन और सोच के विकास के क्षितिज कहाँ तक खुलेंगे, इन सबका ध्यान रखते हुए निर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध करना यह केवल अल्लाह की वह्य का काम है। इसी लिए अल्लामा ने कहा कि यह गहराई जिससे शरीअत विभूषित है, स्वयं शरीअत के सच्चे होने और सच्चाई की एक दलील है। शरीअत की व्याख्या करनेवालों के लेखों में किसी हद तक इस गहराई की झलक नज़र आती है। इमाम ग़ज़ाली हों, हमारे उपमहाद्वीप के हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हों, हज़रत शैख़ अहमद सरहिन्दी मुजद्दिद अल्फ़ सानी हों, इमाम अबू-इसहाक़ शातबी हों या उनसे पहले के मुफ़स्सिरीने-क़ुरआन, हदीस की व्याख्या करनेवाले मुतकल्लिमीने-इस्लाम और इस्लामी फ़ुक़हा हों उन सबके लेखों में यह गहराई पाई जाती है।
दुनिया के बहुत-से क़ानून अभी तक इस गहराई को पहुँचने में नाकाम रहे हैं। जिस तरह उदाहरणार्थ इमाम शातबी ने अपनी किताब ‘अल-मुवाफ़क़ात’ में इस्लामी शरीअत और उसूले-फ़िक़्ह के दर्शन और तत्त्वदर्शिता को स्पष्ट किया है, जितनी गहराई के साथ उन्होंने शरीअत के मौलिक आदेशों की तत्त्वदर्शिताएँ बयान की हैं, जिस विशालता और व्यापकता से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा में शरीअत के रहस्य बयान किए हैं, जितनी समझ और गहराई के साथ मुजद्दिद अल्फ़ सानी, शैख़ अहमद सरहिन्दी ने अपने पत्रों में ‘शरीअत’ और ‘तरीक़त’ की बारीकियों को बयान किया है उसकी मिसालें अंग्रेज़ी क़ानून में, रोमन क़ानून की व्याख्याओं में, अंग्रेज़ी क़ानूनों की व्याख्या में या दुनिया के किसी भी क़ानून की टीका में मिलना अत्यन्त मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ये सब व्याख्याता शरीअत के व्याख्याता हैं, और इसी लिए अपनी गहराई में निराली हैसियत रखते हैं। इसी से शरीअत की एक चौथी विशेषता हमारे सामने आती है, वह उसकी इंसानियत है। आज पश्चिम में इंसान दोस्ती और humanism के नारों की चर्चा सुनकर कुछ ज़ाहिरी चीज़ें ही देखनेवाले शरीअत की इंसानियत को, या शरीअत के इंसानों के दरमियान भूमिका को पश्चिम के humanism या इंसान दोस्ती का एक रूप समझते हैं। यह मात्र ग़लत-फ़हमी है। पश्चिम में जिसको ह्यूमनिज़्म या इंसान दोस्ती कहा जाता है, वह शरीअत की इंसानियत से बिलकुल अलग चीज़ है।
पश्चिम में humanism का अर्थ यह है कि हक़ और बातिल (सत्य-असत्य) का मापदंड कोई आदिकालिक या शाश्वत उसूल नहीं हैं, बल्कि हक़ और बातिल का अस्ल पैमाना इंसान की पसन्द और उसका हित है। जिन चीज़ों को इंसान पसन्द करता है, या जो चीज़ें इंसान के लिए फ़िल्हाल और फ़ौरी तौर पर लाभदायक हैं, वे अच्छी हैं और जो चीज़ें इंसान को नापसन्द हैं और इंसान के तुरन्त लाभ की पूर्ति में अक्षम रहती हैं वे बुरी हैं। गोया अच्छाई और बुराई का मापदंड कोई नैतिक या आध्यात्मिक सिद्धान्त नहीं, कोई स्थायी जीवन संहिता नहीं, बल्कि इंसानों का सामयिक हित और इंसानों की सामयिक पसन्द-ना-पसन्द है। यह धारणा है जिसके आधार पर पश्चिम में नए दर्शन बनाए गए हैं, जिसके आधार पर क़ानूनों के अच्छे या बुरे होने का फ़ैसला किया जा रहा है, जिसके आधार पर आए दिन धारणाएँ बदलती हैं, आए दिन फ़ैशन बदलते हैं, रोज़ाना नए तौर-तरीक़े सामने आते हैं। शरीअत में जिस विशेषता को इंसानियत कहा जा रहा है वह यह सब नहीं है। शरीअत में तो निर्धारित और निश्चित सिद्धान्त यह है कि जिस चीज़ को अल्लाह की शरीअत ने अच्छा क़रार दिया है वह हमेशा के लिए अच्छी है। जिसको बुरा क़रार दिया है, वह हमेशा के लिए बुरी है। इस मापदंड को न इंसानों का सामयिक हित बदल सकता है, न इंसानों की अस्थायी पसन्द-ना-पसन्द बदल सकती है। इसलिए इस अर्थ में तो इंसानियत या ह्यूमनिज़्म की इस्लाम में कोई परिकल्पना नहीं हो सकती।
जिस चीज़ को शरीअत के सन्दर्भ में इंसानियत क़रार दिया जाता है, या कुछ लोगों ने क़रार दिया है उससे मुराद यह है कि शरीअत तमाम इनसानों को एक गिरोह क़रार देती है। आदम की सन्तान या इंसान होने की हैसियत में इंसानों के दरमियान कोई भेदभाव या ऊँच-नीच या अन्तर मौजूद नहीं है और न शरीअत ने इस भेदभाव को स्वीकार किया है। इंसानों का सम्मान “और निस्सन्देह हमने आदम की सन्तान को प्रतिष्ठित किया” (क़ुरआन, 17:70) के विश्वव्यापी एलान के द्वारा हमेशा-हमेशा के लिए कर दी गई है।
मानवता के सम्मान के आधार पर जो भी व्यवस्था बनेगी उसमें न रंग और नस्ल का भेदभाव हो सकता है, न क्षेत्रीय और भाषायी आधार पर अलगाव हो सकता है, न किसी और अस्थायी आधार पर इंसानों को बदला जा सकता है। तमाम इंसानों को एक लड़ी में समो देना आदम की सन्तान को रंग और नस्ल के भेदभाव से परे समझते हुए एक बिरादरी क़रार देना यह शरीअत का एक विशेष गुण और विशेषता है। शरीअत के बहुत-से आदेश इस इंसानी या विश्वव्यापी इंसानियत की अवधारणा पर आधारित हैं।
यह बात आज बहुत ज़ोर-शोर से कही जा रही है कि इंसानों को उनके मौलिक अधिकार दिए जाएँ। आज पश्चिम के बहुत-से लोग मानवाधिकारों के ध्वजावाहक बने हुए हैं। यह एक सुखद बात है, बशर्तेकि मानवाधिकारों के इस नारे से तमाम इंसानों के अधिकार मुराद हों, कुछ विशेष इंसानों या कुछ विशिष्ट नस्लों या धर्मों के माननेवालों के अधिकार मुराद न हों। आज पश्चिम की व्यवस्था में इंसानों की एक संख्या वह है जो दूसरों से बढ़कर इंसान समझे जाते हैं। उनके मुक़ाबले में कुछ इंसान वे हैं जो दरमियाने दर्जे के इंसान माने जाते हैं, कुछ इंसान वे हैं जो सबसे कमतर दर्जे के इंसान माने जाते हैं। इंसानों के प्रति यह भेदभाव और उनका विभाजन पश्चिम की मनोवृत्ति और मानसिकता का हिस्सा है। प्राचीन यूनानी हों या उनके बाद आनेवाले रोमवासी हों, दोनों के यहाँ इंसानों का विभाजन और भेदभाव की कल्पना न केवल मौजूद थी, बल्कि उनकी व्यवस्था का मौलिक अंग थी। अफ़लातून जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक और चिन्तक ने जिसको मुसलमानों ने अत्यन्त निष्पक्षता के साथ सम्मान का पात्र क़रार दिया, जिसको अफ़लातून (अलहि॰) की उपाधि प्रदान की, उसके आदर्श राज्य में ग़ैर-यूनानियों का स्थान सिवाय ग़ुलामी के और कोई नहीं। ग़ैर-यूनानी यूनानियों की ग़ुलामी के लिए इस व्यवस्था में पैदा किए गए हैं।
यही हाल रोमवासियों का था। उनके यहाँ भी ग़ैर-रोमी रोमियों के मातहत और उनकी निगरानी में रहने के लिए ही पैदा किए गए। रोमियों के क़ानून में कोई ऐसी सोच मौजूद नहीं थी कि रोमी और ग़ैर-रोमी बराबर की सतह पर, समान सतह पर किसी एक क़ानून के तहत अपने अधिकार तथा ज़िम्मेदारियों का निर्धारण कर सकें। रोमियों ने अपने लिए अलग क़ानून, यूरोप की गोरी नस्लों के लिए अलग क़ानून और शेष सभी इंसानों के लिए अलग क़ानून बनाए। उन्होंने जिस चीज़ को लॉ आफ़ नेशंज़ (Law of nations) कहा यह वही चीज़ है जिसको प्राचीन शताब्दियों में Droits des gens यानी जन अधिकार के नाम से याद किया गया था। यह वह क़ानून था जो रोमी क़ानूनविदों ने कृपा करके ग़ैर-रोमी क़ौमों के लिए बनाया था। इस क़ानून के तहत शेष तमाम क़ौमों से मामला किया जाता था। यहाँ इस क़ानून के प्रभावों और परिणामों पर चर्चा अभीष्ट नहीं है। इस क़ानून में ग़ैर-रोमियों के लिए क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ प्रस्तावित की गई थीं, क्या-क्या अधिकार प्रस्तावित किए गए थे, यहाँ यह एक अप्रासंगिक सवाल है।
सवाल यह है कि क्या ख़ुद यह धारणा कि ग़ैर-रोमियों के लिए एक अलग क़ानून होना चाहिए मानव समानता की धारणा के विरुद्ध नहीं है? शरीअत ने आरम्भ से ‘ऐ आदम की सन्तान’ कहा ‘ऐ इंसानो’ कहकर एक व्यवस्था, एक जीवन संहिता और एक सिद्धान्त की ओर बुलाया है। शरीअत के सारे आदेश इसी धारणा पर आधारित हैं और कोई ऐसा आदेश शरीअत में, पवित्र क़ुरआन में, सुन्नत में, नहीं पाया जाता जहाँ इंसानों का विभाजन भाषायी, नस्ली या क्षेत्रीय आधार पर किया गया हो। इससे शरीअत का पाँचवाँ विशेष गुण हमारे सामने आता है जो सन्तुलन और मध्यमार्ग है। ज़ाहिर है जब व्यवस्था में गहराई होगी, पकड़ होगी, व्यापकता और सार्वभौमिकता होगी और तमाम इंसानों के हितों और निहितार्थों का ध्यान रखा गया होगा तो इस व्यवस्था में सन्तुलन अपरिहार्य है। अगर सन्तुलन मौजूद न हो तो किसी एक पहलू पर ध्यान बढ़ जाएगा, और दूसरे पहलुओं पर से ध्यान कम हो जाएगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि ज़िन्दगी एक ऐसी डगर पर चल पड़ेगी जो अन्ततः ग़लत साबित होगी, जो आगे चलकर अव्यावहारिक साबित होगी। जिसके परिणाम इंसानों के लिए अनुचित और अलाभकारी होंगे।
इस संक्षेप का विवरण यह है कि इंसानों के विभिन्न ढंग और विभिन्न स्वभाव अतीत में भी रहे हैं। आज भी इंसानों के अन्दाज़ और रंग-ढंग विभिन्न हैं। किसी क़ौम में किसी ख़ास तरह की आदतें पाई जाती हैं। वे आदतें दूसरी क़ौमों में नहीं पाई जातीं। किसी क़ौम में मिसाल के तौर पर आर्ट और उच्च कोटि के साहित्य से अत्यन्त दिलचस्पी पाई जाती है। ईरानी और फ़्रांसीसी इसमें हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। ईरानियों की कला प्रियता और आर्ट से जुड़ाव एक मिसाल बन चुका है। पश्चिमी क़ौमों में फ़्रांसीसियों का यही हाल है। इसके मुक़ाबले में कुछ और क़ौमें हैं जिनको आर्ट और कला से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, बल्कि उनकी दिलचस्पी के मैदान दूसरे हैं। कुछ क़ौमें हैं जो सैन्यकला के मैदान में नुमायाँ हैं और विजेता की शान रखती हैं। उनका इतिहास जंगों और विजयों और सैन्य सफलताओं से भरपूर है। कुछ और क़ौमें हैं जिनमें ज़ाहिर-परस्ती पाई जाती थी। कुछ और क़ौमें हैं जिनमें उच्च विचार, दर्शन और एकाकी धारणाओं से दिलचस्पी की प्रवृत्ति पाई जाती थी।
इस प्रकार ग़ौर किया जाए तो अतीत में भी, सुदूर अतीत में भी और आज भी दुनिया के विभिन्न इलाक़ों और विभिन्न क़ौमों में विभिन्न दिलचस्पियाँ और प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहीं व्यापार से दिलचस्पी है, कहीं कृषि से दिलचस्पी है, कहीं विशुद्ध दार्शनिकता और मात्र वैचारिकता से दिलचस्पी है, कहीं मानव विज्ञान और सामूहिकता से दिलचस्पी है, कहीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी से है। अब अगर इन तमाम दिलचस्पियों में सन्तुलन का ध्यान न रखा जाए तो इस प्रक्रिया में तमाम इंसानों की प्रवृत्तियों का सन्तुलन के साथ ध्यान रखना सम्भव नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी क़ौम इंसानों की विश्वव्यापी व्यवस्था बनाए जिसकी मौलिक रुचि साहित्य और ललित कला से हो तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि मानव जीवन के दूसरे विभाग प्रभावित होंगे। मानव जीवन के दूसरे विभागों के बारे में निर्देश या तो बिलकुल नहीं होंगे, या कम होंगे, या उनका वह महत्त्व नहीं होगा जो समष्टीय रूप से मानव सभ्यता में होना चाहिए। यह सन्तुलन और मध्यामार्ग केवल इस्लामी शरीअत ने दिया है।
एक अजीब और दिलचस्प बात यह है कि इस्लामी शरीअत के सर्वप्रथम ध्वजावाहक वे अरब थे जो हर प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से लगभग अनजान थे। यह अधिकांश आदिवासी थे, बद्दू (देहाती) थे, उनमें से जो विभिन्न बस्तियों में आबाद भी थे वे बहुत सादा और आरम्भिक अर्थव्यवस्था रखते थे। उनकी बस्तियाँ भी छोटी-छोटी थीं और उस ज़माने की सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी उनका कोई विशेष उच्च स्थान नहीं था। सभ्यता और संस्कृति में उनका कोई ऐसा दर्जा नहीं था कि दुनिया को अपनी सभ्यता या संस्कृति से प्रभावित कर सकें। ज़ाहिर है उस ज़माने में भी अरब के लोग व्यापार के लिए विभिन्न देशों में जाया करते थे। दो यात्राओं का उल्लेख तो ख़ुद पवित्र क़ुरआन में मौजूद है “जाड़े और गर्मी की यात्रा” (क़ुरआन, 106:2) यमन और हब्शा व्यापार के क़ाफ़िले जाया करते थे। अरबों के व्यापारिक क़ाफ़िले भारत भी आया-जाया करते थे। अरब के बहुत-से व्यापारी भारत के व्यापारियों से भी सम्बन्ध रखते थे। अरबों के व्यापारिक क़ाफ़िले शाम (सीरिया) और रोमी साम्राज्य में भी जाया करते थे और वहाँ इन लोगों को सम्मान भी मिलता था। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि या उत्प्रेरक केवल व्यापारिक या राजनैतिक हित थे जिसकी वजह से विभिन्न इलाक़ों की सरकारें अरब व्यापारियों को कुछ छूट देती थीं। इस लम्बी व्यापारिक यात्रा के बावजूद, वर्षों के इस सम्पर्क के बावजूद, अरबों के सभ्य या सांस्कृतिक ढंग से कोई अन्तर नहीं पड़ा था। हम कह सकते हैं कि सभ्यता की दृष्टि से अरब एक बिलकुल नौसिखिया और बिलकुल आरम्भिक दर्जे के लोग थे और एक साफ़ और ख़ाली तख़्ती से उनको उपमा दी जा सकती है जिसपर कोई भी छवि नहीं बनी थी। पहली छवि जो अरबों के दिलो-दिमाग़ पर पड़ी वह इस्लाम और शरीअत की छवि थी। अगर शरीअत किसी ऐसी क़ौम को दी जाती, अगर शरीअत के सर्वप्रथम ध्वजावाहक कोई ऐसे लोग होते जो पहले से किसी सभ्यता या संस्कृति से जुड़े होते तो अतीत के सभ्य रवैये, अतीत की सभ्य प्रवृत्तियों, अतीत के सामाजिक ढंग पवित्र क़ुरआन की मौलिकता और पवित्र क़ुरआन की पवित्रता और शरीअत के सिद्धान्तों की मौलिकता को शायद प्रभावित करते। इसलिए शरीअत की सर्वप्रथम छवि ऐसे इलाक़े में रखी गई जहाँ पहले से कोई छवि मौजूद नहीं थी। शरीअत के सर्वप्रथम शब्द वहाँ लिखे गए, उस तख़्ती पर लिखे गए जिस तख़्ती पर पहले कोई अक्षर लिखा हुआ नहीं था। अगर इक्का-दुका कोई अधमिट अक्षर मौजूद थे भी तो वे मिल्लते-इबराहीमी के अक्षर और छापे थे जिनपर शरीअत का आधार निर्मित किया जाना था। इसलिए जब शरीअत की छाप पूर्ण हो गई और शरीअत का मौलिक नक़्शा इंसानों को दे दिया गया तो यह मौलिक नक़्शा मिल्लते-इबराहीमी के अवशेषों के अलावा शेष तमाम प्रभावों से पाक और साफ़ था। न इसपर ईरानी प्रभाव थे, न रोमी प्रभाव थे, न भारतीय वैचारिकता तथा सामाजिकता के आसार थे, न चीनी वैचारिकता तथा सामाजिकता के, वहाँ न पूर्वी प्रभाव थे, न पश्चिमी प्रभाव थे। यह विशुद्ध इस्लामी धारणाओं पर आधारित मिल्लते-इबराहीमी के आधारों पर क़ायम, पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल की रौशनी से रौशन एक कार्य-प्रारूप और नमूना, निर्देश था जिसको लेकर अरब दुनिया में निकले।
अरबों का यानी इस्लाम के सर्वप्रथम ध्वजावाहकों का जब विभिन्न तहज़ीबों से वास्ता पड़ा तो उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं के बारे में कोई विद्वेषपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। इसलिए कि यह विद्वेषपूर्ण रवैया सन्तुलन की धारणा के ख़िलाफ़ होता। सभ्यताओं से, इंसानी विचारों से, सामाजिक मापदंडों और निशानियों से विद्वेषपूर्ण रवैया उस सभ्यता का हो सकता है जिसमें सन्तुलन न पाया जाता हो। जिस सभ्यता में किसी एक पहलू पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया हो वह दूसरे पहलुओं के बारे में आरक्षण रखती है। मिसाल के तौर पर जो सभ्यताएँ विशुद्ध भौतिक विकास के आधार पर क़ायम हैं, जिनमें ज़्यादा ज़ोर भौतिक ज्ञान-विज्ञान और भौतिक साइंस और टेक्नोलॉजी पर है, वे इन सभ्यताओं के बारे में सख़्त आरक्षण रखती हैं जिनमें आध्यात्मिक मूल्यों तथा नैतिक निर्देशो और शिक्षाओं पर भी ज़ोर दिया गया है।
इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस्लामी सभ्यता के सर्वप्रथम ध्वजावाहकों का जब विभिन्न क़ौमों से वास्ता पड़ा तो उन्होंने क्यों विद्वेषपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। दुनिया के सभी विजेताओं के विपरीत अरबों ने पराभूत लोगों के बारे में खुले दिल के साथ जो रवैया रखा, जो उदारता अपनाई वह इस्लाम के इसी सन्तुलन का एक प्रमाण है। ख़ुद खुलफ़ा-ए-राशिदीन हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने, हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने और उनके बाद आनेवाले कई इस्लामी ख़लीफ़ाओं ने ईरान, शाम (सीरिया) और मिस्र की फ़तह के बाद इन इलाक़ों के स्थानीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो स्थानीय प्रशासन रोमी साम्राज्य के ज़माने से शाम (सीरिया) और फ़िलस्तीन में चला आ रहा था उसको ज्यों-का-त्यों जारी रखा। जो स्थानीय प्रशासन ईरान में ख़ुसरुओं, किसराओं (बादशाहों) के ज़माने से चला आ रहा था उसको ज्यों-का-त्यों बाक़ी रखा। यहाँ तक कि ईरान के इलाक़ों में फ़ारसी भाषा स्थानीय सरकारों की भाषा के तौर पर जारी रही। स्थानीय सरकारों के तमाम सरकारी काग़ज़ात और दस्तावेज़ात बदस्तूर फ़ारसी में लिखे जाते रहे। शाम और फ़िलस्तीन के इलाक़ों में यह दस्तावेज़ात और काग़ज़ात स्थानीय भाषा सुरयानी में लिखे जाते रहे। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने, प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) ने इसको अरबी भाषा में परिवर्तित करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। इसलिए कि यह एक विशुद्ध प्रशासनिक चीज़ थी। इसका शरीअत के सर्वव्यापी सांस्कृतिक लक्ष्यों से और उच्च आध्यात्मिक तथा नैतिक उद्देश्यों से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था, न यह चीज़ उसके रास्ते में अवरुद्ध थी। न शरीअत के हितों से टकराती थी। इसलिए यह ज्यों-की-त्यों चलती रही। यह तो बहुत बाद में जाकर ख़लीफ़ा वलीद के ज़माने में तय किया गया कि अब तमाम काग़ज़ात और स्थानीय प्रशासनिक मामलों को अरबी भाषा में लिख लिया जाए। यह फ़ैसला भी एक प्रशासनिक ज़रूरत और निहितार्थ की ख़ातिर किया गया। इस के पीछे कोई भी क्षेत्रीय, भाषागत या नस्ली भावना नहीं थी, बल्कि यह ज़माना वह था कि बड़ी संख्या में लोग इस्लाम क़ुबूल कर चुके थे। स्थानीय भाषाएँ बोलनेवाले रोज़ इस्लाम में दाख़िल हो रहे थे। और नए-नए इलाक़ों से इस्लाम क़ुबूल करके आनेवाले दमिशक़ और उसके आस-पास में आबाद हो रहे थे। यों अरबी जाननेवालों की संख्या बढ़ रही थी और अरबी भाषा एक (lingua franca) के तौर पर तेज़ी से अपनी जगह बना रही थी। इन परिस्थितियों में प्रशासनिक सुविधा और निहितार्थ की अपेक्षा यही थी कि अरबी भाषा को दफ़्तरी ज़बान के तौर पर भी अपना लिया जाए।
इन तमाम अनुभवों से इस सन्तुलन की निशानदेही होती है जिससे मुसलमान हमेशा विभूषित रहे। इस सन्तुलन के सिद्धान्त की रौशनी में अगर मुसलमान और ग़ैर-मुस्लिमों के सम्बन्धों और सम्पर्कों का जायज़ा लिया जाए, विशेष रूप से उन इलाक़ों में जहाँ मुसलमान हमेशा अल्पसंख्या में रहे, उदाहरणार्थ स्पेन और भारत में, तो शरीअत के इस सन्तुलन की बहुत-सी निशानियाँ और अजीब-ग़रीब मिसालें सामने आती हैं।
शरीअत का छठा विशेष गुण स्थायित्व और परिवर्तन के दरमियान सन्तुलन और अन्तर करना है। जहाँ यह शरीअत एक स्थायी शरीअत है, यह दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है और जब तक इस धरती पर या धरती से बाहर इंसान आबाद हैं शरीअत उनके लिए स्थायी जीवन व्यवस्था रहेगी। वहाँ इस शरीअत में नई-नई परिस्थितियों और नई-नई समस्याओं को समो लेने की एक बड़ी अद्भुत क्षमता पाई जाती है।
जो व्यवस्था दृढ़ता और स्थायित्व पर ज़ोर देती हो वह प्रायः परिवर्तन को नज़रअन्दाज़ कर देती है, ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन की माँगें उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं। जो व्यवस्था और विचारधाराएँ परिवर्तन की माँगों का ज़्यादा ध्यान रखती हैं उनकी नज़रों से दृढ़ता और स्थायित्व की माँगें ओझल हो जाती हैं। इसके उदाहरण अतीत के इतिहास में और वर्तमान अवलोकनों में अनगिनत हैं। अतीत में बहुत-सी विचारधाराएँ और धर्म ऐसे मिलते हैं जो ज़माने का साथ नहीं दे सके और ख़त्म हो गए। आज उनकी गिनती प्राचीन अवशेषों में की जाती है। एक ज़माना था कि बाबिल की सभ्यता और बाबिल के क़ानून पूरी दुनिया में एक आदर्श समझे जाते थे। हम्मूरबी (Hammurabi) का क़ानून दुनिया के प्राचीनतम क़ानूनों में संकलित क़ानून का उच्च कोटि का उदाहरण समझा जाता है। इसी तरह दुनिया के विभिन्न स्थानों पर बहुत-से धर्म और विभिन्न विचारधाराएँ प्रचलित थीं। लेकिन आज वे धर्म व्यावहारिक रूप से मौजूद नहीं हैं। ये सब विचारधाराएँ या दर्शन दुनिया से मिट गए। इसका कारण केवल यह है कि उन्होंने अपनी आधारशिला ऐसे नियमों एवं सिद्धान्तों पर रखी जिसमें दृढ़ता और स्थायित्व का तो ध्यान रखा गया था, परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा गया था। ज़माना हरदम बदलता रहता है। हर आनेवाला दिन नई समस्याएँ और मामले लेकर आता है, नई मुश्किलें लेकर आता है। हर आनेवाला समय नए सवालात लेकर आता है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो अपने साथ नई मुश्किलें लेकर आता है। अगर किसी व्यवस्था के पास इन सभी सवालों का जवाब मौजूद न हो, इन नई-नई मुश्किलों का हल मौजूद न हो, इन नए मामलों और नई समस्याओं का हल उसके पास न हो तो उसके लिए ज़िन्दगी में अपना अस्तित्व बरक़रार रखना मुश्किल हो जाता है। और एक मरहला आता है कि वह अपना अस्तित्व खो बैठता है।
इसके मुक़ाबले में आधुनिक काल को देखा जाए तो आधुनिक काल ने शायद यह महसूस किया कि बदलती दुनिया में अपना स्थान बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हर आनेवाले परिवर्तन का साथ दिया जाए, हर नई चीज़ का स्वागत किया जाए और हर आधुनिकता को स्वीकार किया जाए। हर आनेवाले का स्वागत किया जाए और जानेवाले को जल्द-से-जल्द विदा कर दिया जाए। ज़रा ग़ौर कीजिए कि विचारों और क़ानून की दुनिया में अगर यह सिलसिला शुरू हो जाए कि आनेवाली हर चीज़ स्वागत की हक़दार हो और कल की हर चीज़ जो पिछले कल में आई थी, वह अलविदा कहे जाने के लायक़ हो तो दुनिया की किसी व्यवस्था में न सन्तुलन बरक़रार रह सकता है न निरन्तरता बरक़रार रह सकती है। निरन्तरता तो नाम ही है अतीत और भविष्य के दरमियान सम्पर्क को मज़बूत करने का। और यह काम वर्तमान कर सकता है।
सच तो यह है कि वर्तमान का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जिसको हम वर्तमान कहते हैं वह या तो अतीत निकट है या भविष्य निकट। और इन दोनों के दरमियान एक सूक्ष्म विभेदक रेखा पाई जाती है जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जो इस रेखा से निकल गया वह अतीत में शामिल हो गया। जो अभी इस रेखा के नीचे नहीं आया वह भविष्य है, लेकिन इन दोनों के दरमियान मज़बूत सम्बन्ध क़ायम करना यह उसी सूक्ष्म रेखा का काम है जिसको वर्तमान कहा जाता है। अतीत और भविष्य के दरमियान इसी आवश्यक सम्पर्क को बरक़रार रखना उस व्यवस्था का काम है जिसमें दृढ़ता और स्थायित्व के साथ-साथ परिवर्तन की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा गया हो।
इस्लामी शरीअत ने सफलता के साथ इन दोनों माँगों को अपनी व्यवस्था में समोया है। इस्लामी विद्वानों ने, प्राचीन और आधुनिक दोनों ज़मानों में इसपर विस्तार से विचार किया और यह बताया कि स्थायित्व और दृढ़ता क्या है, और परिवर्तन से क्या मुराद है, और यह कि इन दोनों को इकट्ठा कैसे किया जाए। सच्चाई यह है कि इस्लामी शरीअत के इस महत्त्वपूर्ण और मौलिक गुण को आधुनिक काल के बहुत-से आधुनिकतावादी और पश्चिम से प्रभावित चिन्तकों ने समझने में कोताही की है। उन्होंने पश्चिम से प्रभावित अपने अतीत की हर चीज़ को नकारात्मक और वर्तमान की हर चीज़ को सकारात्मक ढंग से देखना शुरू कर दिया है। पश्चिम अपने प्राचीन इतिहास से विरक्त, अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि से रुष्ट, और अपने इतिहास के उतार-चढ़ाव के बारे में असन्तुष्ट है। इसलिए वह अपने अतीत की हर चीज़ को ना-पसन्दीदा और आनेवाली हर चीज़ को पसन्दीदा क़रार देता है, इसलिए कि उसके इतिहास का एक लम्बा दौर जो एक हज़ार साल से अधिक समय पर फैला हुआ है, बल्कि डेढ़ हज़ार साल से अधिक समय पर फैला हुआ है, अन्याय एवं अत्याचार तथा धर्म के नाम पर सख़्त प्रकार की ज़ोर-ज़बरदस्ती से भरा हुआ है। पश्चिम को इस ज़ुल्मो-ज़्यादती और दमन से निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ तक कि स्वयं धर्म की उपेक्षा करनी पड़ी। धर्म की तमाम निशानियों को नकारात्मक क़रार देकर उनसे जान छुड़ाए बिना इस अत्याचारपूर्रण व्यवस्था से बच निकलना पश्चिमवालों के लिए शायद आसान न था। इसलिए पश्चिम की नज़र में, पश्चिम के मनोविज्ञान में, पश्चिम का धार्मिक अतीत एक अत्यन्त नकारात्मक और अप्रिय डरावने स्वप्न जैसा है। जबकि वर्तमान और भविष्य एक लगातार सुखद स्थिति की शुभसूचना देता है। इसलिए पश्चिम ने अतीत की किसी चीज़ से, विशेष रूप से अगर उसका सम्बन्ध धर्म से हो, सम्बन्ध बरक़रार रखना अपनी इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और बनावट की वजह से अनावश्यक समझा।
हमारे बहुत-से लेखक पश्चिम की इस विशिष्ट पृष्ठभूमि को समझे बिना इस्लामी इतिहास पर भी यही धारणाएँ चरितार्थ करना चाहते हैं। और इस तरह इस्लाम के इतिहास की निरन्तरता, शरीअत की आधार और मुसलमानों की दीन की व्यवस्था और दृढ़ता को प्रभावित कर देते हैं। यह बात हम सबको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम का इतिहास इस्लाम से विमुखता का इतिहास नहीं, समष्टीय रूप से इस्लाम का पालन करते रहने का इतिहास है। यह इतिहास मानवता के मानवता पर अत्याचारों और ज़ुल्मो-ज़्यादती का इतिहास नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक सुखद शुभ सूचना की हैसियत रखता है। इस्लाम का इतिहास न्याय एवं इंसाफ़ और सभ्यता और समाज में नई-नई मिसालें क़ायम करने का इतिहास है। इस इतिहास को दोहराने की, इसको ज़िन्दा करने की और आधुनिक काल में एक नए ढंग से इसको जन्म देने की ज़रूरत है। इससे जान छुड़ाना, इसकी उपेक्षा करना और इसको नकारात्मक ढंग से समझना एक बदतरीन प्रकार का नासमझी भी है, मुसलमानों के भविष्य से निराशा का द्योतक भी है और मुसलमानों के अतीत से अनभिज्ञ होने का प्रमाण भी है।
परिवर्तन और दृढ़ता में सन्तुलन के साथ-साथ इस्लामी शरीअत की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता समो लेने की असाधारण क्षमता भी है। इस्लाम की व्यवस्था में चूँकि सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता के साथ-साथ गहराई और सन्तुलन भी है, दृढ़ता और स्थायित्व के साथ-साथ परिवर्तन और परिवर्तन का एहसास भी है। इसलिए इन सब चीज़ों की अनिवार्य अपेक्षा यह भी है कि इस्लाम के स्वभाव में समो लेने की असाधारण क्षमता पाई जाए।
दुनिया की विभिन्न क़ौमों में विभिन्न सभ्यताएँ, विभिन्न संस्कृतियाँ और विभिन्न प्रवृत्तियाँ तथा स्वभाव पाए जाते हैं। किसी भी विश्वव्यापी व्यवस्था के लिए न यह सम्भव है और न उचित कि वह इन तमाम परिवर्तनों को या उन तमाम विविधताओं को समाप्त करके किसी एक सांस्कृतिक धारणा या किसी एक स्वभाव पर तमाम इंसानों को ज़बरदस्ती एकजुट करने की कोशिश करे। यही वजह है कि इस्लामी शरीअत और सभ्यता ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि हर जाति को अपने अन्दर समोया। लेकिन इसके साथ-साथ शरीअत अपनी एकता, अपनी एकजुटता, अपने विशेष गुणों और अपनी निरन्तरता तथा स्थायित्व के बारे में भी अत्यन्त संवेदनशील और अत्यन्त सावधान है। शरीअत किसी ऐसी कार्रवाई को गवारा नहीं करती जिसका नतीजा इस्लाम की निरन्तरता और स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में निकलनेवाला हो। इसलिए इन दोनों की अपेक्षा यह है कि शरीअत हर नई सभ्यता को, आधुनिक रहन-सहन को और हर क़ौम की आदतों और प्रवृत्तियों के विचार और विचारधाराओं के नकारात्मक पहलुओं को अपनी व्यवस्था में इस तरह समो ले कि वह शरीअत की व्यवस्था का अंग बन जाएँ और शरीअत की व्यवस्था को इसी तरह सफलता से चलाने में मदद दें जिस तरह कि वह व्यवस्था इस्लाम के आरम्भिक दौर से चली आ रही है।
जब मुसलमानों का यूनानी ज्ञान-विज्ञान से वास्ता पड़ा तो उन्होंने यूनानी और अफ़लातूनी धारणाओं को इल्मे-कलाम, उसूले-फ़िक़्ह और मुस्लिम-फ़ल्सफ़ा यानी तत्त्वदर्शिता के संकलन के लिए इस तरह प्रयोग किया कि कुछ स्थितियों में यह पता चलाना मुश्किल है कि इन धारणाओं में कौन-सी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से मुसलमान चिन्तकों के ज़ेहन की पैदावार है और कौन-सी चीज़ वह है जो मुसलमानों ने यूनानियों से प्राप्त की है। इसी तरह जब मुसलमान भारत या ईरान में आए तो भारत और ईरान के प्राचीन साहित्य, विचार, धारणाओं में वे तमाम चीज़ें जो सकारात्मक पहलू रखती थीं, जो मानवता की सेवा और मानवता के कल्याण की द्योतक थीं उनको क़ुबूल करने में इस्लामी सभ्यता ने कण बराबर संकोच न किया और इसको तत्त्वदर्शिता क़रार देकर मुसलमानों की गुमशुदा पूँजी क़रार दिया और अपनी व्यवस्था में इस तरह समो लिया कि आज वे चीज़ें इस्लाम के सांस्कृतिक गुलदस्ते का एक महत्त्वपूर्ण फूल हैं।
समो लेने की यह क्षमता वैचारिक, सभ्यता सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में नज़र आती है। फ़ल्सफ़ा (दर्शन) और तत्त्वदर्शिता के मामलात हों, गणित या बौद्धिकता और तार्किकता का विज्ञान हो, चिकित्सा हो, प्रयोगात्मक ज्ञान हो, निर्माण कला हो, कविता एवं साहित्य हो, इन सब मैदानों में मुसलमानों ने दूसरी क़ौमों के समान तत्त्वों से लाभान्वित होने में कभी संकोच नहीं किया। यही वजह है कि इस्लामी सभ्यता बहुत जल्द एक ऐसी विश्वव्यापी सभ्यता बन गई जिसमें तमाम सभ्यताएँ आकर इस तरह समोती चली गईं जिस तरह एक बड़ी नदी में छोटी-छोटी नहरें और छोटे-बड़े दरिया समुद्र में आकर समाते-जाते हैं और यह पता नहीं चलता कि कौन-सा पानी किस नदी से आया था, कौन-सा मोती किस नदी की पैदावार था।
इस्लामी शरीअत की एक और विशेषता उसका वह असाधारण प्रभाव है जो उसने मानव जीवन में पैदा किया है। मानव जीवन को हर पहलू से परिवर्तित करना, मानव जीवन के विभिन्न मामलों को इस तरह अपने रंग में रंग देना कि जीवन का कोई क्षेत्र शरीअत के प्रभाव से बाहर न रहे यह एक ऐसी विशेषता है जिसमें दुनिया की कोई और व्यवस्था शरीअत का मुक़ाबला न अतीत में कर सकी है और न अभी तक कर पाई है।
दुनिया की सभी व्यवस्थाएँ जीवन के किसी एक विशिष्ट पहलू से दिलचपसी रखती हैं। पश्चिमी क़ानूनों का दायरा जीवन के कुछ ख़ास पहलुओं तक सीमित है, जबकि इंसानों की बड़ी संख्या वह है जिनको ज़िन्दगी में कभी भी पश्चिमी क़ानून की किसी धारा से या किसी समस्या से प्रत्यक्ष रूप से वास्ता शायद न पड़ता हो। इसके मुक़ाबले में इस्लामी शरीअत के आदेशों से हर इंसान और हर मुसलमान को ज़िन्दगी में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन सुबह से शाम तक वास्ता रहता है और जब तक वह शरीअत के आदेशों और धारणाओं पर अच्छी तरह कार्यरत न हो, उनसे पूरी तरह परिचित न हो और उनको अपने अन्दर अपनी ज़िन्दगी में समो लेने की भावना न रखता हो उसके लिए शरीअत द्वारा लागू की गई ज़िम्मेदारियों और अपेक्षाओं को पूरा करना मुश्किल है।
यही कारण है कि हर वह व्यक्ति जो शरीअत के कार्यक्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र में आता है उसपर शरीअत के असाधारण प्रभाव पहले दिन से ही सामने आने शुरू हो जाते हैं और ज़िन्दगी के आन्तरिक, वैचारिक, बौद्धिक, सभ्यता सम्बन्धी, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि अन्तर्मानवीय मामलों तक नुमायाँ नज़र आते हैं। आज भी मुसलमानों की बहुत-सी कोताहियों के बावजूद, इस वास्तविकता के बावजूद कि मुसलमानों ने शरीअत पर कार्यान्वयन की अपेक्षाओं को अच्छी तरह पूरा नहीं किया, उसके बावजूद कि आज ग़ैर-इस्लामी धारणाओं का वर्चस्व दिन-प्रतिदिन महसूस होता है, इसके बावजूद कि आज मुस्लिम जगत् के अधिकांश देशों की क़ानूनी व्यवस्था का अधिकांश भाग ग़ैर-इस्लामी धारणाओं के तहत काम कर रहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद इस्लामी शरीअत के प्रभाव और उसकी गहरी छाप हर उस मुसलमान पर महसूस होती है जो किसी-न-किसी हैसियत में शरीअत के किसी पहलू से प्रभावित है। विशेष रूप से पश्चिम जगत् में जो लोग इस्लाम सवीकार करके मुस्लिम समाज का हिस्सा बनते हैं और मुसलमानों के विभिन्न गिरोहों से उनका सम्पर्क होता है, उनकी ज़िन्दगी में जो नुमायाँ, गहरा और तुरन्त परिवर्तन महसूस होता है जिससे पश्चिमवाले भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, यह शरीअत के असाधारण प्रभाव ही की एक निशानी है।
शरीअत की एक और विशेषता जो उसकी विशुद्ध क़ानूनी धाराओं से सम्बन्धित नहीं, बल्कि शरीअत के हर आदेश से सम्बन्धित है, वह शरीअत के आदेशों यानी पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का वह असाधारण उपजाऊपन है जिसका उदाहरण इंसानी सोच के इतिहास में छिपा है। इस उपजाऊपन की निशानी वे अनगिनत आदेश और असंख्य आंशिक फ़तवे और इज्तिहादात हैं जो शरीअत की सीमित नुसूस (स्पष्ट आदेशों) और पवित्र क़ुरआन की अत्यन्त सीमित आयतों और कुछ हज़ार हदीसों पर आधारित हैं।
हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि शरीअत के व्यावहारिक भाग का नाम फ़िक़्ह है। यानी शरीअत के आदेशों का वह हिस्सा जो इंसान के ज़ाहिरी मामलों और समस्याओं से बहस करता हो, फ़िक़्ह के कार्यक्षेत्र में आता है। पवित्र क़ुरआन की छः हज़ार छः सौ आयतों में से केवल दो सौ या तीन सौ के क़रीब आयतें वे हैं जो आदेश की आयतें कहलाती हैं। यानी जो प्रत्यक्ष रूप से फ़िक़ही आदेशों पर रौशनी डालती हैं और जिनसे प्रत्यक्ष रूप से फ़िक़ही आदेश निकलते हैं। उतनी ही संख्या उन आयतों की भी होगी जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से फ़िक़ही आदेश निकाले गए हैं। इस तरह पवित्र क़ुरआन की वे सभी ‘नुसूस’ जिनसे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से फ़िक़्ह के आदेश निकाले गए है, उनकी संख्या किसी भी सूरत में पाँच सौ से ज़्यादा नहीं। यही बात आदेशों से सम्बन्धित हदीसों के बारे में कही जा सकती है कि आदेशों की हदीसों की संख्या कुल हदीसों के मुक़ाबले में उतनी ही है जितनी पवित्र क़ुरआन की कुल आयतों के मुक़ाबले में आदेशों की आयतों की है। कुल हदीसें जिनकी संख्या सब मिलाकर ज़्यादा-से-ज़्यादा पचास हज़ार के क़रीब है उनमें फ़िक़ही हदीसें कुछ हज़ार, तीन या चार हज़ार के लगभग से ज़्यादा नहीं हैं। ये कुछ हज़ार ‘नुसूस’ मानव जीवन के असीमित और असंख्य मामलों और आदेशों को अनुशासित करते हैं।
इस अनुशासन का व्यावहारिक विवरण अगर देखा जाए तो उससे अन्दाज़ा होता है कि अर्थों और मतलबों का कितना असीमित समुद्र है जो इन सीमित ‘नुसूस’ में छिपा है। मिसाल के तौर पर पवित्र क़ुरआन की केवल तीन आयतों की रौशनी में इस्लामी फ़ुक़हा ने पूरा इल्मे-मीरास संकलित किया है जिसमें प्रतिष्ठित फ़ुक़हा के आंशिक मतभेदों की भी बहुत गुंजाइश है, इन आंशिक मतभेदों की वजह से आदेशों और फ़तवों में विविधता भी पैदा हुई है, इसमें व्यापकता और अधिकता भी पैदा हुई है। लेकिन इस व्यापकता और अधिकता को नज़रअन्दाज़ करते हुए, मतभेदों को नज़रअन्दाज़ करते हुए अगर मात्र विरासत के आदेशों की व्यापकता पर नज़र डाली जाए तो आश्चर्य होता है कि केवल तीन आयतों के आधार पर ये हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों स्थितियाँ जो विरासत के विभिन्न आदेशों को बयान करती हैं केवल इन तीन आयतों के आधार पर संकलित की गई हैं।
इस्लामाबाद में एक माहिर और निष्ठावान कंप्यूटर इंजीनियर जनाब बशीर अहमद बगवई ने एक ऐसा सॉफ़्टवेअर तैयार किया है जिसमें विरासत की दो करोड़ स्थितियों की कल्पना करके, यानी 20 मिलियन स्थितियों को काल्पनिक रूप से शामिल करके उन सबके जवाबात को समोया गया है और उन दो करोड़ स्थितियों के सम्भावित आदेश पवित्र क़ुरआन की इन्हीं तीन आयतों से निकलनेवाले नियमों और सिद्धान्तों की रौशनी में बयान किए गए हैं। यह सॉफ़्टवेअर जो अपने प्रकार का शायद पहला सॉफ़्टवेअर है शरीअत की इस व्यापकता, असाधारण प्रभाव, उपजाऊपन और समो लेने की क्षमता का असाधारण द्योतक है।
इसी तरह से इस्लाम के दीवानी और फ़ौजदारी आदेशों पर अगर नज़र डाली जाए तो ये दीवानी और फ़ौजदारी आदेश पवित्र क़ुरआन की कुछ आयतों से लिए गए हैं। इन कुछ सौ आयतों पर और कुछ हज़ार हदीसों पर पिछले चौदह सौ साल से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के ज़माने से विद्वान ग़ौर करते चले आ रहे हैं, और आदेशों और उनके विवरणों का एक न थमनेवाला सिलसिला है जो आज तक जारी है। जिन-जिन देशों में इस्लाम का क़ानून फ़ौजदारी प्रचलित है वहाँ आए दिन उन सीमित आयतों और हदीसों के आधार पर मामलों के फ़ैसले हो रहे हैं और कभी भी कोई रुकावट या मुश्किल या दिक़्क़त महसूस नहीं हुई।
अतीत में उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक, बल्कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मुस्लिम जगत् के एक हिस्से में शरीअत के दीवानी और फ़ौजदारी आदेशों का बड़ा हिस्सा लागू था। उस समय भी पवित्र क़ुरआन की इन कुछ सौ आयतों और कुछ हज़ार हदीसों से किए हुए लाखों और हज़ारों व्यक्तिगत इज्तिहादात, कथन और फ़तवे इस पूरी व्यवस्था को जो मराक़श से लेकर इंडोनेशिया के पूर्वी द्वीपों तक, और साइबेरिया की सीमाओं से लेकर ज़ंजबार और तंज़ानिया की सीमाओं तक फैला हुआ था, सफलतापूर्वक चला रहे थे। इस पूरे क्षेत्र में फ़िक़्हे-इस्लामी के अनुसार कामयाबी से हुकूमतों की व्यवस्था चल रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी क़ायम थे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी पूरी दुनिया में फैला हुआ था। दुनिया के समुद्रों पर मुसलमान व्यापारियों और मुसलमान मल्लाहों का कंट्रोल था और वे यह सारी व्यवस्था इस्लामी शरीअत और इस्लामी क़ानूनों के अनुसार चला रहे थे।
शरीअत की एक और महत्त्वपूर्ण बल्कि अति महत्त्वपूर्ण विशेषता बौद्धिक तर्कों और लिखित आदेशों का एक ऐसा मेल है जो दुनिया के किसी और धार्मिक क़ानून में नहीं पाया जाता। पूरी इस्लामी शरीअत और फ़िक़्हे-इस्लामी इस मेल का एक सुन्दर नमूना है। लेकिन सबसे ज़्यादा यह मेल शरीअत के जिस पहलू में नज़र आता है वह इस्लाम का इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह है। इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह जो एक ही समय में इस्लामी बौद्धिकता का और इस्लामी बौद्धिक पन्थ का सबसे बड़ा नमूना है वहाँ वह एक ही समय में इस्लामी नक़्लियात (लिखित आदेशों) का और मुसलमानों के धार्मिक क़ानून, व्यवस्था और दर्शन का भी सबसे व्यापक और सबसे पूर्ण नमूना है।
यह कहा जाए तो ग़लत न होगा कि दुनिया के धार्मिक और बौद्धिक इतिहास में उसूले-फ़िक़्ह के समतुल्य कोई और कला ऐसी मौजूद नहीं है जो इतनी गहराई, इतनी व्यापकता और इतनी विशालता के साथ बुद्धि तथा लिखित आदेशों, दोनों की अपेक्षाओं को एक साथ पूरा करती हो। बौद्धिक अपेक्षाओं के पूरा करने का हाल यह है कि इल्मे-उसूले-फ़िक़्ह के पहली पंक्ति के प्रतिनिधियों ने यूनानी ज्ञान और तार्किकता और बौद्धिकता से काम लेकर उसूले-फ़िक़्ह को इस तरह संकलित किया कि इस ज़माने का बौद्धिकता का बड़े-से-बड़ा प्रतिनिधि उसूले-फ़िक़्ह के किसी आदेश या किसी सिद्धान्त पर तर्क या बुद्धि के दृष्टिकोण से आपत्ति न कर सका।
इसी तरह उसूले-फ़िक़्ह के आदेश जो मौलिक रूप से पवित्र क़ुरआन और हदीसों से लिए गए हैं वे प्रत्यक्ष रूप से एक धार्मिक ज्ञान और धार्मिक क़ानून की हैसियत रखते हैं। इसलिए दीनियात (धर्मशास्त्र) और उलूमे-नक़्लिया (हदीस, इतिहास और फ़िक़्ह आदि का ज्ञान) की सभी अपेक्षाएँ भी उसूले-फ़िक़्ह में बहुत अच्छी तरह मौजूद हैं।
उसूले-फ़िक़्ह की इस दौर की किताबों का जायज़ा लिया जाए जिसमें उसूले-फ़िक़्ह अपनी परिपक्वता और पराकारष्ठा को पहुँचा यानी पाँचवीं शताब्दी हिजरी से लेकर दसवीं शताब्दी हिजरी तक का ज़माना तो वे एक साथ अक़्ल और नक़्ल दोनों का पूरे तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इमाम ग़ज़ाली की ‘अल-मुस्तसफ़ा’ हो या इमाम राज़ी की ‘अल-महसूल’, इमाम शातबी की ‘अल-मुवाफ़क़ात’ हो या उनके उस्ताद इमाम क़राफ़ी की किताबें ‘अल-फ़ारूक़’ वग़ैरा, इन सबमें जहाँ एक तरफ़ उलूमे-नक़्लिया की पराकाष्ठा नज़र आती है कि पवित्र क़ुरआन और हदीसों से निकलनेवाले आदेशों को इस कलात्मक ढंग से इतने सटीक ढंग से संकलित किया उसकी मिसाल दुनिया के दूसरे धर्मों के क़ानूनों में नहीं मिलती, वहाँ ये किताबें इस्लाम की धार्मिक बौद्धिकता की भी उच्चतम प्रतिनिधि की हैसियत रखती हैं और मुसलमानों के वैचारिक पन्थ के उत्कृष्ट उदाहरण की हैसियत रखती हैं। जहाँ तार्किकता और दर्शन की धारणाओं और तर्क शैली को इस तरह उसूले-फ़िक़्ह का हिस्सा बनाया गया कि अधिकांश स्थितियों में इन किताबों को समझना उस समय तक सम्भव नहीं जब तक पढ़नेवाला यूनानी तर्कशास्त्र तथा यूनानी ज्ञान-विज्ञान की धारणाओं से पूरे तौर पर परिचित न हो।
फिर जैसे-जैसे मुसलमानों में वैचारिक विकास और बौद्धिकता की कला विकसित होती गई और मुसलमान ‘मश्शाई दर्शन’ के साथ-साथ ‘इशराक़ी दर्शन’ को भी अपनी वैचारिकता के तराज़ू में जगह देते गए उसी गति और उसी ढंग से ये धारणाएँ इस्लाम के धार्मिक ज्ञान में विशेष रूप से उसूले-फ़िक़्ह में झलकती पाई गईं। एक ज़माना था कि जब पूर्व में मुल्ला सिदरा, पश्चिम में इब्ने-ख़लदून और इमाम शातबी और इस तरह के दूसरे विद्वानों ने उसूले-फ़िक़्ह और मुसलमानों की बौद्धिकता तथा वैचारिक पन्थों को व्यापक और भरपूर तरीक़े से संकलित कर दिया था। उस समय तक के खोजे गए सभी ज्ञान-विज्ञान और उस समय तक मुसलमानों के संकलित सभी बौद्धिक और ज्ञानपरक कारनामों को उसूले-फ़िक़्ह के संकलन में इस तरह प्रयोग किया गया कि उनमें से हर पहलू एक साथ इस्लामी फ़िक़्ह, इस्लामी सोच, इस्लामी शरीअत और उसूले-फ़िक़्ह के सेवक के रूप में काम करता नज़र आता है। एक न्यायप्रिय समीक्षक तुरन्त महसूस कर लेता है कि किस तरह बौद्धिकता और नक़्लियात (धर्मग्रन्थों से उद्धृत आदेश) दोनों को इस तरह व्यापकता के साथ एक-दूसरे में समोया गया है कि इसकी मिसाल दुनिया में किसी और धर्म के इतिहास में नहीं मिलती।
इस्लामी शरीअत के बारे में एक और वास्तविकता ज़ेहन में रहनी चाहिए। यह वास्तविकता अगर नज़रअन्दाज़ हो जाए तो शरीअत के मामले में कभी-कभी ग़लत-फ़हमी या उलझन पैदा हो सकती है, वह यह है कि शरीअत मौलिक रूप से एक व्यावहारिक व्यवस्था है। इंसान के व्यावहारिक जीवन का सुधार करना, इंसान की ज़िन्दगी को बेहतर बनाना, इंसानों की ज़िन्दगी को नैतिकता और न्याय एवं इंसाफ़ के आधार पर क़ायम करना, इंसानों के बौद्धिक जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को जारी करना और एक ऐसा समाज क़ायम करना जो नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो, यह शरीअत का मौलिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जहाँ अनिवार्य होता है वहाँ शरीअत में विशुद्ध वैचारिक या बौद्धिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन ऐसी बौद्धिक समस्याएँ, या ऐसे विशुद्ध बौद्धिक अथवा अनूठे प्रश्न जिनका कोई व्यावहारिक परिणाम ज़ाहिर न होनेवाला हो, उनसे बहस करना शरीअत के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। शरीअत के स्वभाव समझनेवाले प्रसिद्ध विद्वान इमाम शातबी ने एक जगह लिखा है कि शरीअत हर उस समस्या की उपेक्षा करती है जिसपर कोई कार्यान्वयन होनेवाला न हो। इस प्रक्रिया में ज़ाहिरी कर्म भी शामिल हैं और हार्दिक या आन्तरिक कर्म भी शामिल हैं। आन्तरिक कर्मों से अभिप्रेत वे नैतिक गुण या वे आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ हैं जो शरीअत को अभीष्ट हैं। अगर किसी विचार या अक़ीदे के परिणामस्वरूप वे प्राप्त होती हैं तो वह विचार या अक़ीदा शरीअत की नज़र में ध्यान देने योग्य है। इसके विपरीत ऐसी विशुद्ध बौद्धिक चर्चाएँ जिनका कोई व्यावहारिक परिणाम सांसारिक जीवन में निकलनेवाला न हो उनपर विचार-विमर्श करना, और उन सवालों को उठाना शरीअत ने अनावश्यक और अलाभकारी क़रार दिया। एक प्रसिद्ध हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने बयान किया कि अल्लाह की सृष्टि पर चिन्तन करना सही है, लेकिन अल्लाह के अस्तित्व पर चिन्तन करना अनुचित है।
अल्लाह तआला की सृष्टि पर चिन्तन-मनन करने से इंसान को नैतिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं और भौतिक लाभ भी उपलब्ध हो सकते हैं जिनको हम आए दिन देखते रहते हैं। लेकिन अल्लाह तआला का अस्तित्व हमसे बिलकुल ओझल है। इंसान की समझ के लिए, इंसान के विवेक के लिए उसकी हैसियत अत्यन्त गुप्त जैसी है। इंसान की सीमित बुद्धि इंसान की सीमित समझ और इंसान का सीमित विवेक अल्लाह के अस्तित्व की वास्तविकता को समझ नहीं सकता। इसलिए जो चीज़ इंसान के वश से बाहर है उसपर ग़ौर करना समय की बर्बादी नहीं तो और क्या है? शरीअत के इस स्वभाव को देखते हुए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने, बल्कि ख़ुद पवित्र क़ुरआन ने ईमानवालों का यह प्रशिक्षण किया कि वे केवल वही सवालात उठाएँ जिनकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता हो, और अगर कोई ऐसा सवाल किसी के ज़ेहन में आए जो विशुद्ध वैचारिक प्रकार का हो तो उसका वह जवाब दिया जाए जिसका व्यावहारिक परिणाम निकलनेवाला हो। मिसाल के तौर पर पवित्र क़ुरआन में एक जगह सवाल नक़्ल किया गया है— “ये लोग आपसे पूछते हैं कि क़ियामत कब आएगी?” (क़ुरआन, 79:42) इसके जवाब में यह नहीं बताया गया कि क़ियामत कब आएगी, या कब तक नहीं आएगी, अल्लाह तआला ने इसको अपने इल्म में सुरक्षित रखा है। इंसानों को क़ियामत के समय से बाख़बर करना अल्लाह तआला की तत्त्वदर्शिता और मशीयत (नियति) के ख़िलाफ़ है। इसलिए इस तरह के तमाम सवालात पूरी तरह अव्यावहारिक प्रश्न हैं। उनके जवाब में पवित्र क़ुरआन ने पूछा, तुम यह बताओ कि तुम्हारा दर्जा या तुम्हारा स्थान क़ियामत को याद रखने के बारे में क्या है? क्या तुमने क़ियामत के सवाल-जवाब को याद रखा है? क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यह है वह सवाल जो इंसानों को करना चाहिए और जिसके व्यावहारिक परिणाम उनके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ ज़ाहिरी और भौतिक जीवन में भी सामने आ सकते हैं।
एक और मौक़े पर कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा, “ऐ अल्लाह के रसूल! क़ियामत कब आएगी?” नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इसके जवाब में किसी अक़ीदे या नज़रिए की बात नहीं की। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, “तुमने क़ियामत के लिए क्या तैयारी की है?”
इसी तरह से कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पवित्र क़ुरआन में सवाल नक़्ल किया गया है जिनके विस्तृत और स्पष्ट उत्तर दिए जा सकते थे। लेकिन उस समय तक इंसान का ज्ञान और अवलोकन क्षमता इस दर्जे तक नहीं पहुँची थी कि पवित्र क़ुरआन के बहुत-से सर्वप्रथम श्रोता उससे लाभ उठा सकते। उदाहरणार्थ पूछा गया, यह चाँद का निकलना, उसका घटना-बढ़ना यह सब क्या है? इसके जवाब में पवित्र क़ुरआन ने किसी कलात्मक या वैज्ञानिक टीका को बयान करने की ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि वह जवाब दिया जिससे चौदह सौ साल पहले का एक आम अरब भी फ़ायदा उठा सकता था, आज का इंसान भी फ़ायदा उठा सकता है और आगे आनेवाला इंसान भी हर दौर में इस सवाल को अपने लिए सार्थक पाएगा। “कह दीजिए कि यह चाँद का घटना-बढ़ना और इसका कम-ज़्यादा होना यह लोगों के लिए वक़्तों के निर्धारण में सहयोगी होता है और हज के समयों और तारीख़ों का इससे अन्दाज़ा होता है।” गोया यह बताया गया कि इबादतों के समयों का निर्धारण चाँद के महीनों से होता है। इसलिए इबादतों के मामले में चाँद का अत्यन्त महत्त्व है। रुयते-हिलाल और चाँद निकलना, ये सारी चीज़ें न केवल वक़्तों के निर्धारण में बल्कि कई इस्लामी इबादतों के निर्धारण में महत्त्व रखती हैं।
यही कारण है कि इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) और उलमाए-उसूल ने स्पष्ट रुप से लिखा है कि ग़ैर-ज़रूरी बौद्धिक बहसों को उठाना, विशेष रूप से दीनी मामलों में, यह शरीअत के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। इमाम शातबी ने लिखा है “आम लोगों के सामने शरीअत की हक़ीक़तों की गहराइयाँ बयान करना सही नहीं है, इसलिए कि यह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और गुज़रे हुए नेक बुज़ुर्गों के स्वभाव के ख़िलाफ़ है। इसकी वजह यह है कि शरीअत तो सबके लिए है। शरीअत जहाँ ग़ज़ाली और राज़ी जैसे उच्चतम दिमाग़ों के लिए है वहाँ एक आम इंसान के लिए भी है। वह चौदह सौ साल पहले के रेगिस्तान के एक देहाती अरब के लिए भी थी और आज के सुसभ्य इंसान के लिए भी है। इसलिए अगर शरीअत में ये सवालात उठाए गए होते तो यह अतीत में बहुत-से लोगों के लिए उलझन का कारण बनते और आज भी अधिकाँश लोगों के लिए उलझन और ग़लत-फ़हमी ही का कारण होते।
गहरे और गूढ़ प्रश्न जनसाधारण के स्वभाव और आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होते, इसलिए पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) ने और विशेष रूप से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शरीअत ने इन सवालात को ध्यान देने योग्य नहीं समझा।
इस चर्चा से यह न समझा जाए कि इस्लाम के स्वभाव में दार्शनिकतापूर्ण चिन्तन की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है, पवित्र क़ुरआन में, शरीअत में, कुछ ऐसे संकेत मौजूद हैं जिनसे काम लेकर इस्लामी चिन्तकों ने कलाम, फ़लसफ़ा और हिकमत पर ढेरों किताबें लिख डालीं। लेकिन यह सब कुछ एक सीमित वर्ग के लिए था। इन किताबों की ज़रूरत न अच्छा मुसलमान बनने के लिए है, न किसी व्यक्ति को नैतिक ऊँचाइयाँ प्राप्त करने के लिए इन गहरी बातों को जानने की ज़रूरत है, न किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए इन गहराइयों में जाने की ज़रूरत है। इन गहराइयों की हैसियत इल्म के दस्तरख़ान की चटनी की है। अगर किसी को दिलचस्पी है तो इस चटनी से फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दस्तरख़ान के तमाम खानों को नज़रअन्दाज़ कर दे और सिर्फ़ चटनी को काफ़ी समझने लगे तो वह अपनी सेहत का दुश्मन होगा।
इसलिए यह देखना चाहिए कि मानव जीवन के विभिन्न दर्जे, चरण और दिलचस्पियाँ क्या हैं और उनके बारे में शरीअत का रवैया क्या है। चूँकि यहाँ गहराई और सोच की बात आ गई इसलिए उचित यह मालूम होता है कि आगे बढ़ने से पहले यह देखा जाए कि इल्म के बारे में शरीअत क्या कहती है और शरीअत की सोच ज्ञान के अनिवार्य और ज़रूरी होने के बारे में क्या है।
यह बात तो हम सब जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति शरीअत में अनिवार्य है। हदीस में है कि “इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है।” इस एक हदीस के अलावा अनगिनत क़ुरआनी आयतें और हदीसें ऐसी हैं जिनमें इल्म के महत्त्व को बार-बार बताया गया है। इन आयतों और हदीसों से हर मुसलमान परिचित है जिनको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। उनसे अन्दाज़ा होता है कि शरीअत में इल्म की हैसियत क्या है। शरीअत की बुनियाद दो चीज़ों पर है। एक इल्म दूसरे अद्ल (न्याय)। शरीअत का मौलिक उद्देश्य, जैसा कि पवित्र क़ुरआन की एक आयत में स्पष्ट रूप से आया है, वास्तविक न्याय और इंसाफ़ की स्थापना है। “और निस्सन्देह हमने अपने रसूलों को स्पष्ट निशानियाँ देकर इसी लिए भेजा और उनके साथ ईशग्रन्थ और तुला इसी लिए उतारी कि लोग वास्तविक अद्ल और इंसाफ़ पर क़ायम हो जाएँ।” (क़ुरआन, 57:25) गोया पवित्र क़ुरआन के अनुसार ये सभी आसमानी किताबों का सर्वप्रथम उद्देश्य और मूल लक्ष्य रहा है कि मानव समाज में वास्तविक न्याय और इंसाफ़ क़ायम हो जाए, पूर्ण न्याय और इंसाफ़ क़ायम हो जाए। पूरी तरह न्याय और इंसाफ़ क़ायम करने के लिए ज़रूरत है कि समाज में ज्ञान एवं विवेक का स्तर मौजूद हो। अगर ज्ञान और विवेक का स्तर समाज में दरकार दर्जे का न हो तो फिर उस समाज में पूर्ण न्याय और इंसाफ़ क़ायम करना मुश्किल होता है।
पवित्र क़ुरआन के अनुसार इंसान अल्लाह का ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) है। ख़िलाफ़ते-इलाहिया (अल्लाह के प्रतिनिधित्व) का पात्र होने की क्षमता उसमें ज्ञान के कारण पैदा हुई। जैसा कि आदम (अलैहिस्सलाम) के वृत्तान्त से स्पष्ट होता है। “और उस (अल्लाह) ने आदम को सभी चीज़ों के नाम सिखाए”, (क़ुरआन, 2:31) अत: ज्ञान और न्याय दोनों इंसान के अस्तित्व के उद्देश्य से सम्बन्ध रखते हैं। इंसान का फ़रिश्तों और अन्य सृष्टि से श्रेष्ठ होना, इंसान का स्थान और रुतबा और इंसान की हैसियत ज्ञान ही के आधार पर क़ायम हुई है। और इंसानों के मार्गदर्शन के लिए जो शरीअत दी गई उसका सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्वप्रथम उद्देश्य न्याय है। गोया आरम्भ ज्ञान और चरम न्याय है। न्याय पर इस सिलसिले में चर्चा आगे चलकर होगी। जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है इसके तीन दर्जे हैं। एक दर्जा वह है जो फ़र्ज़े-ऐन कहलाता है और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस दर्जे को बयान करने के लिए तीन शीर्षक अपनाए जा सकते हैं। एक शीर्षक है “मा तसह्हु बिहिल-अक़ीदा” यानी इल्म का, इल्मे-दीन का, शरीअत के इल्म का इतना हिस्सा जिसके ज़रिये इंसान का अक़ीदा और ईमान दुरुस्त हो जाए। ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ और ‘ईमाने-मुजमल’ की शब्दावलियाँ इस्लाम के आरम्भ के विद्वानों ने ज्ञान के इस दर्जे को आसान बनाने के लिए और इसको एक कैप्सूल में बंद करने के लिए अपनाई हैं। दूसरा दर्जा या दूसरी शब्दावली है “मा तसह्हु बिहिल-इबादा” हर इंसान पर इबादत फ़र्ज़ है। आज एक व्यक्ति इस समय मुसलमान हो तो कुछ घंटों के बाद उसपर ज़ुह्र की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरह से कुछ महीनों बाद रमज़ान का महीना आएगा और रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर सामर्थ्यवान है तो कुछ महीनों के बाद हज का मौसम आ जाएगा तो हज करना चाहिए। अगर सामर्थ्यवान है तो साल भर बाद ज़कात देना पड़ेगी। इसलिए इबादतों से छुटकारा किसी सक्षम इंसान के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए “मा तसह्हु बिहिल-इबादा” भी ज़रूरी है। यानी शरीअत का इतना इल्म ज़रूर प्राप्त होना चाहिए कि अनिवार्य और ज़रूरी इबादात इंसान अदा कर सके।
तीसरा दर्जा है “मा तसह्हु बिहिल-मईशत” जिसके द्वारा उसकी रोज़ी-रोटी और ज़िन्दगी दुरुस्त हो जाए। इस दर्जे में शरीअत का ज्ञान भी शामिल है और दुनिया का ज्ञान भी। इंसान का सम्बन्ध जिस पेशे से है या समाज के जिस कार्यक्षेत्र से है, उस कार्यक्षेत्र का ज्ञान ज़रूरी है। अगर कोई इंसान सम्बन्धित और ज़रूरी ज्ञान के बिना कोई पेशा अपनाता है तो अव्वल तो वह सफल नहीं होगा और अगर भौतिक दृष्टि से सफल हो भी जाए तो यह एक बहुत बड़ा ख़तरा है जो वह अपनी ज़ात और दूसरों के लिए पैदा कर रहा है। इस ख़तरे के नतीजे में अगर किसी को नुक़्सान हो गया तो शरीअत उसको जुर्माना अदा करने का हक़दार क़रार देगी। एक हदीस है जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि अगर किसी इंसान ने डॉक्टरी का पेशा अपनाया और वह मेडिकल का ज्ञान नहीं रखता था और उससे किसी का नुक़्सान हो गया तो उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ेगा। किसी की जान चली गई तो उसको ‘दियत’ (अर्थदंड) देना पड़ेगी। इसी तरह से दूसरे मामलों को भी समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ का कलात्मक ज्ञान जो उस दौर, उस ज़माने और इस क्षेत्र की दृष्टि से अनिवार्य हो उसको प्राप्त करना भी शरीअत के अनुसार अनिवार्य है, और ख़ुद इस मैदान के बारे में शरीअत का ज्ञान भी ज़रूरी है। एक व्यक्ति कृषि का काम करता है तो जहाँ कृषि के तौर-तरीक़े उसको जानने चाहिएँ वहाँ उसको कृषि के बारे में शरीअत के आदेश भी जानने चाहिएँ। एक व्यक्ति व्यापार का पेशा अपनाता है तो जहाँ व्यापार के प्रचलित तरीक़े उसको आने चाहिएँ वहाँ उसको व्यापार के इस्लामी आदेश भी जानने चाहिएँ।
यह तो ज्ञान का वह हिस्सा है जो हर व्यक्ति को अनिवार्य रुप से प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का दूसरा हिस्सा वह है जिसे इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने फ़र्ज़े-किफ़ाया क़रार दिया है। फ़र्ज़े-किफ़ाया में भी ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। शरीअत का ज्ञान भी शामिल है और दुनिया का ज्ञान भी। दुनिया के ज्ञान के सिलसिले में इमाम ग़ज़ाली, अल्लामा इब्ने-तैमिया और इस्लाम के दूसरे बड़े विद्वानों ने लिखा है कि इन तमाम ज्ञान-विज्ञान, इन तमाम उद्योगों और महारतों का जानना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़े-किफ़ाया है जिनकी मुस्लिम समाज को ज़रूरत हो और जिनके न जानने की वजह से मुस्लिम समाज की आत्म निर्भरता प्रभावित हो, और मुस्लिम समाज दूसरों पर निर्भर हो जाए। इस तरह के ज्ञान-विज्ञान, उद्योग और निपुणताएँ हर दौर की हिसाब से बदलती रहेंगी। हर दौर के हिसाब से जिन निपुणताओं की मुस्लिम समाज को ज़रूरत होगी, विशेष रूप से मुस्लिम समाज की आज़ादी और आत्म निर्भरता की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी महारतें दरकार हों वे महारतें प्राप्त करना मुस्लिम समुदाय के लिए फ़र्ज़े-किफ़ाया होगा। इसी तरह शरीअत की महारत का वह दर्जा प्राप्त करना भी फ़र्ज़े-किफ़ाया है जहाँ आम लोगों को ज़रूरी दीनी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, जनसाधारण अपनी उन समस्याओं का जवाब मालूम कर सकें जिनका जवाब हर व्यक्ति के पास नहीं होता, जो अनिवार्य दीनी शिक्षा की सतह से परे चीज़ें हैं, उनका ज्ञान समाज में कुछ लोगों के पास होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि शरीअत एक विशुद्ध व्यावहारिक व्यवस्था है। शरीअत अव्यावहारिक माँगें नहीं करती। शरीअत इंसानों से वह कुछ करने को नहीं कहती जो इंसान के वश में न हो। शरीअत हर एक से यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति फ़क़ीह और मुज्तहिद हो जाए। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) अपने ज़माने में एक ही थे। इस्लामी चिन्तकों में से जिसका भी नाम लें उनकी मिसाल उनके ज़माने में या तो वे ख़ुद ही थे या उन जैसे कुछ और लोग थे। मुसलमानों की अधिकांश संख्या ज्ञान और चिन्तन की उस सतह पर नहीं थी जिस तरह पर अपने ज़माने में इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी, शाह वलीउल्लाह या और दूसरे लोग थे। यहाँ तक कि ख़ुद प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में सबकी सतह एक नहीं थी। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की संख्या लाखों में है। एक लाख चालीस हज़ार या चौबीस हज़ार सहाबा तो वे थे जिन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ आख़िरी हज में शिरकत की। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का मुबारक दीदार किया। ज़ाहिर है इन सब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में से हर एक शैख़ैन के मक़ाम और मर्तबे का नहीं था, हर एक ज्ञान के उस दर्जे पर नहीं था जिसपर हज़रत अली आसीन थे। हर एक दीन के गहरे इल्म और फ़िक़ही मामलात तथा शरीअत के व्यावहारिक मामलों में महारत का वह दर्जा नहीं रखता था जो दर्जा हज़रत अबदुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हु) का या हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ियल्लाहु अन्हु) का या दूसरे बड़े सहाबा का था।
इसलिए शरीअत हर एक से यह नहीं कहती कि हर व्यक्ति फ़िक़्ह और दक्षता के इस स्थान पर पहुँच जाए जिसपर बहुत थोड़े लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन हर मुस्लिम समाज में ऐसे लोग मौजूद होने चाहिएँ जिनसे मुस्लिम समाज सम्पर्क कर सके, मुस्लिम समाज अपने मार्गदर्शन के लिए उनके ज्ञान से फ़ायदा उठा सके।
इस दर्जे की भी दो सतहें हैं, एक सतह तो तुलनात्मक रूप से आम और निचले दर्जे की सतह है जो आम लोगों के लिए दरकार है। एक आम इंसान को आए दिन ऐसी समस्याओं से वास्ता पेश आता रहता है जिनका जवाब उसके पास नहीं होता। उसने शरीअत का जो अनिवार्य ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान में उसका जवाब नहीं मिलता। इसलिए उसको ज़रूरत महसूस होती है कि किसी बड़े विद्वान से मार्गदर्शन प्राप्त करे। यह ज़रूरत किसी को कम महसूस होती है किसी को ज़्यादा, किसी को रोज़ाना किसी को कभी-कभी किसी को बहुत ज़्यादा किसी को कभी-कभार, लेकिन इस बात की ज़रूरत सबको पड़ती है कि किसी ज्ञानवान से मार्गदर्शन प्राप्त करे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीअत ने आदेश दिया है कि हर गिरोह, हर जमाअत, हर वर्ग, हर बस्ती, हर शहर में कुछ लोग ऐसे होने चाहिएँ जिनकी संख्या का निर्धारण उसी बस्ती या उस इलाक़े या उस गिरोह की आवश्यकताओं की दृष्टि से होगा। जो दीन (धर्म) में गहरी समझ रखते हों, सबका इस काम के लिए निकलना ज़रूरी नहीं, कुछ लोग निकलें। एक, दो, तीन, पाँच, दस पंद्रह आवश्यकतानुसार ऐसे लोगों का निकलना काफ़ी है जो दीन में गहरी समझ प्राप्त करें, गहरी अन्तर्दृष्टि और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करें और यह प्राप्त करने के बाद अपने लोगों को जिस वर्ग से वे गए हैं उस वर्ग के लोगों को दीनी मार्गदर्शन दे सकें।
यह बात मुस्लिम समाज के ज़िम्मे फ़र्ज़े-किफ़ाया है कि वह इसका प्रबन्ध करे कि समाज में ऐसे लोग मौजूद हों, समाज में शरीअत के ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हों जो जनसाधारण के मार्गदर्शन का कर्त्तव्य भली प्रकार निभा सकें। जिस तरह मुस्लिम समाज के ज़िम्मे यह फ़र्ज़े-किफ़ाया है कि इसमें चिकित्सा विशेषज्ञों की ऐसी संख्या में मौजूद हो जो जनसाधारण का इलाज कर सकें। ऐसे इंजीनियर मौजूद हों जो कलात्मक मामलों और इंजीनियरिंग के मामलों में मुस्लिम समाज की ज़रूरत को पूरा कर सकें, ऐसे निर्माण विशेषज्ञ मौजूद हों जो मुस्लिम समुदाय की निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हों जो विभिन्न क्षेत्रों और कलाओं में मुसलमानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, यह बात केवल शरीअत की निपुणताओं के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि तमाम निपुणताओं के साथ है। शरीअत के बारे में इन निपुणताओं का महत्त्व और भी अधिक है, इसलिए कि इंसान की और मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी का दारोमदार शरीअत पर और इस्लाम से जुड़ाव पर है।
इस मामले में एक शाफ़िई फ़क़ीह अल्लामा ख़तीब अश-शरबीनी ने और दूसरे अनेक शाफ़िई फुक़हा ने बड़ी महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प बात लिखी है। सम्भव है दूसरे फ़िक़ही मकातिब (विचारधारा) के लोगों ने भी लिखी हो, शाफ़िई फ़ुक़हा ने लिखा है कि यह ज़रूरी है कि हर ‘अदवा’ की मुसाफ़त (सफ़र की दूरी) पर एक मुफ़्ती मुक़र्रर किया जाए। एक ऐसा आलिम जो दीनी मामलात में मार्गदर्शन या फ़तवा दे सके वह हर ‘अदवा’ की मुसाफ़त पर मौजूद होना चाहिए। ‘अदवा’ से मुराद उन्होंने यह लिया है कि इतनी मुसाफ़त या इतना क्षेत्रफल या इलाक़ा जिसमें कोई व्यक्ति सुबह फ़ज्र की नमाज़ के बाद आवश्यकताओं से निवृत होकर पैदल चल पड़ा हो, सम्बन्धित शरीअत के विशेषज्ञ, आलिम या मुफ़्ती से मुलाक़ात करे। पैदल जाकर, अपनी समस्या बयान करे, मार्गदर्शन प्राप्त करे और सूर्यास्त से पहले-पहले पैदल अपने घर वापस आ सके। यह शर्त इसलिए रखी कि हर व्यक्ति के पास सवारी नहीं होती, बहुत-से लोगों को पैदल ही आना-जाना पड़ता है। शरीअत किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ पर मजबूर नहीं करती जिसपर कार्यान्वयन के संसाधन उसके पास न हों। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास आज गाड़ी हो, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के पास प्राचीन ज़माने में घोड़ा या ख़च्चर या ऊँट मौजूद हो। इसलिए एक स्वस्थ इंसान एक आम स्वस्थ इंसान कम-से-कम उस ज़माने में ऐसा था कि पैदल जाए तीन, चार, पाँच मील, आठ मील और जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करके वापस आ जाए। इस फ़ासले तक जाने-आने में कोई कष्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि ऐसी समस्याएँ रोज़ पेश नहीं आएँगी, कभी-कभार ही पेश आएँगी। कभी-कभार इस तरह का सफ़र करके चला जाना यह कोई बहुत मेहनत की या मुश्किल बात नहीं है।
आज की दृष्टि से हम कह सकते हैं, क्योंकि यातायात के साधन बहुत हैं, ये साधन तेज़-रफ़्तार और आम हैं और हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं कि हर बड़े शहर में कम-से-कम कुछ ऐसे विद्वान मौजूद होने चाहिएँ जिन तक जनसाधारण मार्गदर्शन के लिए सम्पर्क कर सकें। हर छोटी बस्ती में एक-एक, दो-दो ऐसे लोग ऐसे होने चाहिएँ। अगर सरकारें यह प्रबन्ध करें, ऐसी शिक्षण संस्थाएँ क़ायम करें, इस्लामी शोधकार्य और शिक्षा की उच्च संस्थाएँ हों, जामिआत हों, कुल्लियात सरकारी और हुकूमती संसाधनों से क़ायम हों तो बहुत अच्छी बात है। वर्ना अगर सरकारें इसमें कोताही करेंगी तो वे अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगी। लेकिन जनसाधारण इस ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे। फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे ख़ुद आगे बढ़ें और ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ क़ायम करें। जहाँ-जहाँ ऐसी ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ क़ायम हैं, जैसे पाकिस्तान में, तो उनकी मदद करना, इन संस्थाओं को और विकास देना यह जनसाधारण की ज़िम्मेदारी है।
फ़र्ज़-किफ़ाया के इस दर्जे के साथ एक दर्जा और भी है जो फ़र्ज़े-किफ़ाया का भी फ़र्ज़े-किफ़ाया है। यह वह दर्जा है कि जहाँ ख़ुद विद्वानों को मार्गदर्शन की ज़रूरत पेश आती है। वे विद्वान जो जनसाधारण का मार्गदर्शन कर रहे हों, अगर ख़ुद उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत पेश आ जाए तो वे कहाँ सम्पर्क करें। और यह कि ऐसे नए मामले और समस्याएँ जो मुस्लिम समाज को पेश आएँ उनका जवाब मुस्लिम समाज कहाँ से मालूम करे। कुछ समस्याएँ ऐसी हो सकती हैं कि ये विशेषज्ञ और मुफ़्ती लोग जो जगह-जगह, बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव उपलब्ध हैं, वे समस्याएँ उनकी सतह से ऊपर की हों। अगर उनकी सतह से ऊपर की समस्याएँ पेश आ जाएँ तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे भी मुस्लिम समाज में होने चाहिएँ जो इन नए मामलात का जवाब दे सकें। इज्तिहादी सूझ-बूझ रखते हों, विशेष योग्यता और आलोचनात्मक ढंग से आधुनिक काल की समस्याओं और मुश्किलों को जानते हों। अपने ज़माने की आवश्यकताओं और माँगों से परिचत हों। ज़माने की प्रवृत्तियों पर गहरी नज़र रखते हों। समय को पहचानते हों। फ़िक़्ह और शरीअत के स्वभावश को पहचानते हों। दीन में गहरी अन्तर्दृष्टि रखते हों। पवित्र क़ुरआन, सुन्नते-रसूल और शरीअत के पूरे भंडार से विशेषज्ञ की भाँति परिचित हों। ज़ाहिर है ऐसे लोग बड़ी संख्या में नहीं होंगे। ऐसे लोग थोड़े ही होंगे, अतीत में भी थोड़े थे। अभी मैंने मिसाल दी कि इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) अपने ज़माने में एक ही थे या उन जैसे कुछ और लोग होंगे, लेकिन ऐसे विशेषज्ञ उस ज़माने की दृष्टि से भी बहुत थोड़े थे। यह फ़र्ज़े-किफ़ाया का एक बहुत ऊँचा दर्जा है। शरीअत के मामलात में, बल्कि शरीअत के अलावा अन्य तमाम मामलों में भी ऐसे लोगों के उपलब्ध होने का प्रबन्ध करना मुस्लिम समाज की ज़िम्मेदारी है। यह तो फ़राइज़ (कर्त्तव्यों) के वे दर्जात हैं जो ज्ञान के बारे में शरीअत क़रार देती है। अद्ल (न्याय) के बारे में बाद में बात करेंगे।
इन अनिवार्य तक़ाज़ों के साथ-साथ शरीअत ज्ञान-विज्ञान के विकास, सोच की व्यापकता, साहित्य और सभ्यता के विकास को पसन्द करती है और उसको प्रोत्साहित करती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन उपलब्ध करने को पसन्दीदा और अच्छा बताती है। लेकिन यह ज्ञान का वह दर्जा है जिसको कुछ बुज़ुर्गों ने ज्ञान की चटनी क़रार दिया है। इमाम शातबी के शब्दों में यह “मिल्हुल-इल्म” (इल्म का नमक) हैं। मिसाल के तौर पर विशुद्ध साहित्यिक मामले, शरीअत के आदेशों से निकलनेवाले बहुत-से ऐसे पहलू जिनका दर्जा तत्त्वदर्शिता और निहितार्थ की खोज का है, या भाषा-शैली की बारीकियाँ हैं, बुज़ुर्गों के रवैये को आधार बनाने का मामला है, तसव्वुफ़ के कुछ दर्जे हैं, किसी ख़ास ज्ञान एवं कला के मैदान में विशेष रूप से लाभ उठाने के मामलात हैं, ये वे चीज़ें हैं कि अगर सारी क़ौम उन विवरणों ही की प्राप्ति पर लग जाए तो ज्ञान और सोच का सन्तुलन बिगड़ जाएगा, ऐसी सूरत में असन्तुलन पैदा हो जाता है और समाज सही दिशा पर क़ायम नहीं रह सकता। हम उपमहाद्वीप की मिसाल लें, उपमहाद्वीप में जब मुसलमानों के पतन का दौर था, तो हर पढ़ा-लिखा आदमी, समाज का हर शिक्षित व्यक्ति शेअरो-शाइरी पर लगा हुआ था। शेअरो-शाइरी ही भारत के लोगों का उठना बैठना थी। शरीअत शेअरो-शाइरी को नापसन्दीदा नहीं क़रार देती। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) में भी शेअरो-अदब से दिलचस्पी रखनेवाले लोग मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) शाइरी और साहित्य के बड़े आलिम थे, हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ख़ुद भी कभी-कभी शेअर कहा करते थे। हज़रत अबदुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) शेअरो-शाइरी से बहुत दिलचस्पी रखते थे। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) को बहुत-से शेअर याद थे। लेकिन उनकी हैसियत ‘मिल्हुल-इल्म’ की थी। इन बुज़ुर्गों के इस रवैये से स्पष्ट होता है कि जाहिल अरबों के वे अशआर जो पवित्र क़ुरआन या सुन्नत को समझने के लिए अनिवार्य हों उनसे दिलचस्पी रखने में कोई हरज नहीं।
यह ज्ञान का वह दर्जा था जिसको इस्लामी विद्वानों ने इल्म के दस्तरख़ान की चटनी या ‘मिल्हुल-इल्म’ (इल्म का नमक) से उपमा दी है। ये वे मामलात हैं जो न जनसाधारण के लिए फ़र्ज़ हैं, न प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों के लिए अनिवार्य और ज़रूरी हैं, न इज्तिहाद करने और शरई आदेश निकालने में प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई ज़रूरत है। लेकिन यह इल्म और समझदारी के वे पहलू हैं जिनसे इस्लामी सभ्यता पूर्ण होती है, जिनसे इस्लाम की वैचारिक और बौद्धिक संस्कृति की शान में वृद्धि होती है और ज्ञान-विज्ञान के नए-नए आयाम और नए-नए विकास सामने आते हैं। इसलिए अगर प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों में से कुछ लोग और विद्वानों की एक सीमित संख्या इन समस्याओं पर ध्यान दे तो वह शरीअत की नज़र में एक पसन्दीदा काम है। लेकिन अगर मुसलमानों की बड़ी संख्या या मुसलमानों का अधिकांश भाग अपने ध्यान को इन चीज़ों पर केन्द्रित कर ले तो फिर न केवल दीन, बल्कि जीवन के दूसरे महत्त्वपूर्ण पहलू प्रभावित होने का सम्भावना रहती है। और ज्ञान तथा चिन्तन की दुनिया के वे महत्त्वपूर्ण मामले प्रभावित हो सकते हैं जिनपर धार्मिक अथवा दुनयवी सफलता का दारोमदार है। शरीअत के बारे में यह बात पहले भी कही जा चुकी है और पवित्र क़ुरआन में कई जगह इसको स्पष्ट रूप से बयान किया गया है कि जहाँ तक दीन के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, ये तमाम पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) में एक रहे हैं। और तमाम आसमानी किताबों में, पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) की शिक्षा में, और पैग़म्बरों (अलैहिमुस्सलाम) के साथ आनेवाले पैग़ाम में इन्ही सिद्धान्तों की शिक्षा थी और अपने ज़माने और परिस्थितियों की दृष्टि से तमाम प्रतिष्ठित पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) ने इन उसूल और इन्ही बुनियादों का विवरण बयान किया।
हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी (रह॰) ने एक जगह मक्तूबात में, मक्तूबात के भाग प्रथम के पत्र नंबर 63 में, इस बात पर विस्तार से रौशनी डाली है कि पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) उसूले-दीन (धर्म के मौलिक सिद्धान्तों) में किस तरह एकराय हैं और उसूले-दीन में मतैक्य के बाद शरीअतों में मतभेद और शरीअतों में विवरण किस तरह विविध होते हैं, यह बात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने, इमाम शातबी (रह॰) ने, इमाम ग़ज़ाली (रह॰) ने, अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) ने और शरीअत का स्वभाव पहचाननेवाले अनेक विद्वानों ने विस्तार से बयान की है।
इन सब चीज़ों के साथ जो बात सामने रहनी चाहिए वह यह है कि शरीअत का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है, बल्कि अगर यह कहा जाए कि मूल उद्देश्य है तो ग़लत न होगा कि इंसानों को उनकी निजी पसन्द-ना-पसन्द, अपने भौतिक निहितार्थों और निजी लाभों के दायरे से निकालकर एक सर्वव्यापी शरीअत के अनुशासन में लाया जाए, यह शरीअत के मूल उद्देश्यों में से एक या सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। इमाम शातबी (रह॰) ने इसके लिए शब्दावली प्रयोग की है ‘इख़राजुल-मुकल्लिफ़ अन-दाइयतुल-हवा’ यानी जितने सक्षम इंसान हैं जिनको अल्लाह तआला ने शरीअत की ज़िम्मेदारी का पाबन्द बनाया है उन सबको हवस और मन की इच्छाओं के दायरे से निकालकर शरीअत के दायरे में लाना, यह शरीअत का मौलिक उद्देश्य है।
उद्देश्यों पर चर्चा के साथ-साथ यह याद रखना ज़रूरी है कि उद्देश्यों की व्याख्या अगर इंसान अपने निजी हितों को देखते हुए करने लगे, इंसानी जान-माल की सुरक्षा अगर हर व्यक्ति अपने निजी हित को देखते हुए, हर क़ौम अपने क़ौमी हितों के पहलू से, हर क़बीला और हर बिरादरी अपने गिरोही हितों की दृष्टि से करने लगे तो यह शरीअत के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि शरीअत के उद्देश्यों से फिर जाना होगा। इसलिए कि यह तमाम उत्प्रेरक वे हैं जो मन की इच्छाओं से जन्मी भावना पर आधारित हैं। इसलिए शरीअत ने सबसे पहले जिस चीज़ का रास्ता रोका है, वह मन की इच्छा पर चलने का रास्ता है जिससे इंसानों को दूर करना ज़रूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अक़ाइद (धार्मिक अवधारणाओं) से काम लिया गया, नैतिकता से भी काम लिया गया, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रशिक्षण से भी काम लिया गया, और फिर आख़िर में शरीअत के आदेशों की प्रवृत्ति भी यही है कि इंसानों को निजी हित, निजी इच्छाओं और निजी पसन्द-ना-पसन्द के प्रयोग के लिए सीमाओं का पाबन्द बनाया जाए। यहाँ तक कि अगर किसी नेक काम में भी निजी हित शामिल हो जाए, किसी इबादत में भी मन की इच्छाएँ शामिल हो जाएँ, सांसारिक निहितार्थ शामिल हो जाएँ, तो इसका रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक होता है और वह चीज़ प्रिय से हट कर धीरे-धीरे अप्रिय होने तक ले जाती है। उदाहरण के रूप में नमाज़ सबसे श्रेष्ठ इबादत है। लेकिन अगर नमाज़ रियाकारी (दिखावे) की ख़ातिर पढ़ी जाने लगे, नमाज़ इसलिए पढ़ी जाने लगे कि लोग बुज़ुर्ग और वली क़रार दें, तो यह अमल बहुत ग़लत रास्ता इख़तियार कर लेता है। और यह विशुद्ध आध्यात्मिक चीज़ भी शरीअत की नज़र में अत्यन्त अप्रिय हो जाती है।
अगर एक बार मन की इच्छा का रास्ता खुल जाए तो इससे हीलों (बहानों) का रास्ता खुल जाता है। और इंसानी ज़ेहन और स्वभाव ऐसे-ऐसे तरीक़े सुझाता है जिसमें शरीअत के ज़ाहिरी आदेशों की पाबन्दी तो नज़र आए, लेकिन शरीअत के उद्देश्य और लक्ष्य एक-एककर प्रभावित हो जाएँ।
ये वे मौलिक नियम और धारणाएँ हैं जिनपर अल्लाह की शरीअत का दारोमदार है। इन मौलिक नियमों एवं सिद्धान्तों से प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों की बड़ी संख्या ने बहस की है। इन बहसों में जिन विद्वानों का नाम बहुत नुमायाँ है उनमें इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी, इमाम क़राफ़ी, अल्लामा इज़ुद्दीन-बिन-अब्दुस्सलाम अस-सुलमी, अल्लामा इब्ने-तैमिया, अल्लामा इब्नुल-क़य्यिम, इमाम शातबी, और इन सबके साथ-साथ हमारे उपमहाद्वीप के हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी शामिल हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ के पहले हिस्से में उन क़वाइद और मौलिक धारणाओं का विस्तार से उल्लेख किया है जिनसे शरीअत के महत्त्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य निकाले जाते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर वे निहितार्थ खोजे जाते हैं जिनपर शरीअत के आदेशों का दारोमदार है।
शाह वलीउल्लाह का काम इस दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्त्व रखता है कि उन्होंने केवल मुसलमानों को सम्बोधित नहीं किया, बल्कि अपने ज़माने की पूरी इल्मी दुनिया को और दुनिया के तमाम चिन्तकों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपनी चर्चा की उठान उन सिद्धान्तों पर रखी जो इस ज़माने की दृष्टि से बौद्धिक जगत् के निर्धारित सिद्धान्त और निर्धारित धारणाएँ थीं। चुनाँचे उन्होंने सबसे पहले बताया कि ‘तकलीफ़ शरई’ (शरई रुप से किसी कार्य का पाबन्द करने) के कारण क्या होते हैं। अल्लाह तआला क्यों किसी को किसी कार्य का पाबन्द करता है? और तकलीफ़ या मुकल्लफ़ (पाबन्द) बनाए जाने से मुराद क्या है? फिर अल्लाह तआला ने बदला देने का जो सिलसिला रखा है, प्रतिदान और सज़ा की व्यवस्था की है, वह क्यों की है और उसका प्रकार क्या है। इस ज़िन्दगी में इनाम और सज़ा की इस परिकल्पना का क्या महत्त्व है, आख़िरत की ज़िन्दगी में यह दंड और इनाम किस प्रकार का होगा? ज़ाहिर है कि इस सारी चर्चा का सम्बन्ध मानव जीवन और उसके विकास से बहुत गहरा है, फिर जब दुनिया में इनाम और सज़ा की बात होगी तो यह भी देखना पड़ेगा कि मानव मानसिक दृष्टि से किस सतह पर खड़ा है। सभ्यता और संस्कृति के किस स्थान पर है और अपने मानसिक स्तर, वैचारिक उच्चता और साधारण जीवन-प्रणाली की दृष्टि से कितनी स्वच्छता और कोमलता का मालिक है।
सभ्यता तथा संस्कृति की इन सतहों को शाह वलीउल्लाह ने ‘इर्तिफ़ाक़ात’ के शब्द से बयान किया है। इर्तिफ़ाक़ का शब्द जो शाह साहब के यहाँ प्रयुक्त हुआ है, कुछ नया है। बहुत-से लोगों को उसे समझने में उलझन पेश आई है। लेकिन इससे मुराद सांस्कृतिक विकास के वे प्रतीक हैं जो मानव जीवन में नज़र आते हैं। शाह साहब ने अपने इतिहास के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक पहल के ये दर्जे या सभ्यता सम्बन्धी विकास के ये चरण चार होते हैं। पहला चरण वह होता है जब इंसान बहुत आरम्भिक जीवन से एक आदिवासी जीवन की ओर क़दम बढ़ा रहा होता है और मानव जीवन अपने सभ्य एवं सांस्कृतिक स्तर की दृष्टि से बहुत आरम्भिक स्तर पर होता है। यह आरम्भिक स्तर भी वह होता है जिसमें कुछ सिद्धान्त साझे होते हैं, कुछ नैतिकता और आध्यात्मिकता के शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है और कोई मानव समाज उनसे ख़ाली नहीं होता।
यहाँ शाह साहब ने इन पश्चिमी विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से मतभेद किया है, जिन्होंने बिना किसी तर्क और बिना किसी ज्ञानपरक आधार के इंसानों के आरम्भ के बारे में बहुत-सी बेसिर-पैर की बातें गढ़ ली हैं। उन्होंने मान लिया है कि इंसान अपने आरम्भ में अत्यन्त पाशविक और असभ्य था और हैवानी अन्दाज़ की ज़िन्दगी रखता था। उन्होंने यह भी मान लिया कि इंसान किसी नैतिकता और नियम का पाबन्द नहीं था। यह मात्र कल्पनाएँ हैं जिनका कोई बौद्धिक या ऐतिहासिक आधार नहीं है। चूँकि आज पश्चिम जगत् में अधार्मिकता और सेक्युलरिज़्म का चलन है, धर्म से दूरी और नफ़रत आम है इसलिए पश्चिमी ज़ेहन इन धारणाओं को आसानी से क़बूल कर लेता है। इसलिए ये सभी अनुमान और निराधार अनुमान पश्चिम के ज्ञान जगत् में सर्वमान्य सत्य का दर्जा पा गए।
शाह साहब के लेख, विशेषकर ‘इर्तिफ़ाक़ात’ की बहस में एक नया दृष्टिकोण सामने आता है जिसका आधार गहरे अवचेतन, अध्ययन और बौद्धिक सिद्धान्तों पर है। ‘इर्तिफ़ाक़ात’ की इस धारणा के आधार पर शाह साहब ‘सआदत’ से बहस करते हैं। ‘सआदत’ से मुराद वह सर्वप्रथम लक्ष्य है या वह आख़िरी उद्देश्य है जो हर इंसान अपने सामने रखता है। ‘सआदत’ की शब्दावली क़रीब-क़रीब (happiness) की शब्दावली के समानान्तर शब्दावली है जो पश्चिमी चिन्तक और यूनानियों ने अपनाई थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों और रोमन चिन्तकों के नज़दीक ख़ुशी इंसानों के लिए महान उद्देश्य या महान कृपा की हैसियत रखती है जिसको पश्चिमी सोच की शब्दावली में ‘सम्मम बोनम’ (Summum Bonum) कहते हैं। अगर यह महान कृपा Happiness या ख़ुशी है तो ख़ुशी और प्रसन्नता आम तौर पर एक भौतिक और पाशविक चेतना या शारीरिक आभास को कहते हैं जिसका सम्बन्ध बहुत आसानी से मन की इच्छाओं से जोड़ा जा सकता है। चुनाँचे ख़ुद प्राचीन यूनानियों में जहाँ happiness यानी ख़ुशी को इंसानों का मूल उद्देश्य क़रार दिया गया वहाँ बहुत जल्द ऐसी धारणाएँ पैदा हो गईं जहाँ केवल भौतिक सुख-सुविधाओं, भौतिक प्रसन्नता और भौतिक आनन्द की प्राप्ति ही को इंसान का उद्देश्य क़रार दिया गया था।
इस्लामी चिन्तकों ने ख़ुशी या happiness या उसके समानार्थी कोई शब्दावली प्रयोग नहीं की, बल्कि ‘सआदत’ की विशुद्ध क़ुरआनी शब्दावली प्रयोग की, ‘सईद’ और ‘सआदत’ विशुद्ध क़ुरआनी शब्दावलियाँ हैं। ‘शक़ी’ और ‘सईद’ का विभाजन पवित्र क़ुरआन ने जगह-जगह किया है। इसलिए ‘सआदत’ की शब्दावली में जो गहरी आध्यात्मिकता, स्पष्ट नैतिक मूल्य और व्यापकता एवं सार्थकता पाई जाती है वह किसी और शब्दावली में नहीं पाई जाती। इसी परम्परा को अपनाते हुए शाह साहब ने ‘सआदत’ की शब्दावली प्रयोग की है और यों उन्होंने ‘सआदत’ का सिलसिला (जो विशुद्ध दार्शनिक अवधारणा के तौर पर सामने आई थी) इल्मे-कलाम और शरीअत के उद्देश्यों से जोड़ा है। एक तरफ़ शाह साहब उसका रिश्ता नेकी और गुनाह की बहस से जोड़ते हैं यानी किस चीज़ को शरीअत में गुनाह क़रार दिया गया और किस चीज़ या किस काम को शरीअत में नेकी क़रार दिया गया, दूसरी तरफ़ ‘सआदत’ की बहस को शरीअत के उद्देश्यों से जोड़ते हैं।
नेकी और बुराई अक़ीदों और कलाम (तार्किकता) के महत्त्वपूर्ण विषय हैं, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मूल विषय हैं। लेकिन इन नैतिकता और तार्किकता के विषयों का अत्यन्त गहरा सम्बन्ध मुसलमानों के सामूहिक जीवन यानी सामुदायिक राजनीति से है जिससे शरीअत के उद्देश्य उभरते हैं और शरीअत के सारे आदेशों की पूर्ति होती है। इस तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी (रह॰) ने हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा के पहले भाग में शरीअत के उद्देश्यों या आदेशों के निहितार्थ की एक बहुआयामी, वैचारिक, सभ्य, ज्ञानपरक और सांस्कृतिक आधार उपलब्ध कर दिया है। यहाँ शाह वलीउल्लाह अपने से पहले के सभी विद्वानों और अपने समकालीन विद्वानों में सबसे अलग नज़र आते हैं।
शरीअत के उद्देश्यों और निहितार्थों पर जब चर्चा होती है तो यह बात कुछ लोग भूल जाते हैं कि इन निहितार्थों और उद्देश्यों का सम्बन्ध केवल इस सांसारिक जीवन से नहीं है, बल्कि दरअस्ल इन सबका सम्बन्ध आख़िरत की ज़िन्दगी से है। इसलिए कि शरीअत का स्वभाव और मौलिक उद्देश्य और शरीअत की ज़िम्मेदारी डाले जाने का मूल उद्देश्य और लक्ष्य इंसान के पारलौकिक जीवन को सफल बनाना और इस दुनिया की ज़िन्दगी को इस दृष्टि से संगठित और संकलित करना है कि परलोक में इसके सकारात्मक प्रभाव हों, यह शरीअत के उद्देश्यों और शरीअत के निहितार्थों का मौलिक लक्ष्य है।
शरीअत के ये नियम एवं सिद्धान्त पूर्णतः निश्चित और यक़ीनी हैं। इसलिए कि उनकी बुनियाद शरीअत के सिद्धान्तों पर है जो पूर्णतः प्रमाणित हैं। दूसरी ओर उसूले-अक़्लिया (बौद्धिक सिद्धान्तों) से भी उनका समर्थन होता है और स्पष्ट बात है कि जो चीज़ बुद्धि की दृष्टि से भी प्रमाणित हो और नक़्ल (लिखित सिद्धान्तों) की दृष्टि से भी निश्चित रूप से प्रमाणित हो उसके निश्चित और यक़ीनी होने में क्या शक हो सकता है? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन निश्चित सिद्धान्तों के अन्तर्गत आनेवाले आंशिक आदेश भी सब एक-एक करके निश्चित हैं, यह ज़रूरी नहीं है, कुछ आंशिक आदेश अनुमानित भी हो सकते हैं। जैसा कि शरीअत का हर विद्यार्थी जानता है। लेकिन किसी सिद्धान्त के अधीन मामले या आंशिक समस्या के अनुमानित होने का यह मतलब नहीं है कि ये आंशिक आदेश जिन सिद्धान्तों के तहत आ रहे हैं वे सिद्धान्त निश्चित नहीं हैं।
इस्लामी शरीअत ने, जैसा कि बताया गया, ज़िन्दगी के हर पहलू और मानव जीवन की सभी सम्भावित अपेक्षाओं पर ध्यान दिया है। जिस तरह इंसान के शरीर को भोजन और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसी तरह इंसान के दिल को भी भोजन और दवा दोनों की ज़रूरत है। शरीअत भोजन भी है, शरीअत दवा भी है, शरीअत अपने आदेशों और अपने आम सिद्धान्तों और मार्गदर्शन की दृष्टि से इंसानी दिलों के लिए भोजन है, इंसानी दिलों के लिए ताक़त है। इंसान शरीअत पर जितना अमल करते जाएँगे उनके दिल उतने साफ़ और पाकीज़ा होते जाएँगे।
दिलों के साफ़ और पाकीज़ा होने के लिए ज़रूरी है कि शरीअत के तथ्य सामने रहें, उद्देश्य सामने रहें। केवल ज़ाहिरी अनुपालन और शाब्दिक बाज़ीगरी पर ध्यान न हो, बल्कि दरअस्ल शरीअत की रूह पर अमल करने की नीयत हो और खुले और छिपे दोनों तरह के अमल को समान रूप से सामने रखा गया हो।
शरीअत का मूल उद्देश्य, जैसा कि बताया गया, दिलों के लिए भोजन और दवा दोनों का उपलब्ध कराना है। जिस तरह दिल का सम्बन्ध इंसान के अंगों से बहुत गहरा होता है, उसी तरह इंसान के अन्तर्मन का सम्बन्ध भी इंसान के ज़ाहिर से बहुत गहरा होता है। अन्तर्मन के प्रभाव इंसान के ज़ाहिर पर और ज़ाहिर के प्रभाव इंसान के अन्तर्मन पर होते हैं। यह आए दिन देखने में आता है। इंसान अपने ज़ाहिर में बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है जिसके प्रभाव उसके अन्तर्मन पर पड़ते हैं। इसी तरह उसके अन्तर्मन में कुछ ऐसी धारणाएँ और विचार पैदा होते हैं, ऐसे विचार और भावनाएँ जन्म लेती हैं जिनके प्रभाव उसके ज़ाहिर पर तुरन्त ही महसूस हो जाते हैं।
इसलिए शरीअत ने सबसे पहले तहारत और पाकीज़गी दोनों पर ज़ोर देते हुए दिल और जिस्म दोनों की पाकीज़गी और बाहर और अन्दर दोनों की पाकी को निश्चित बनाने की कोशिश की है। पवित्र क़ुरआन ने जहाँ जिस्म और लिबास को ज़ाहिरी नापाकियों से बचाने और पाक करने और पाक रखने का आदेश दिया है, जहाँ जिस्म को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं, वहाँ दिल और रूह को भी नैतिक बुराइयों से पाक करने का आदेश दिया है। दिल और ज़मीर (अन्तर्रात्मा) को अल्लाह के अलावा दूसरों का केन्द्र बनने से बचाना और केवल अल्लाह के लिए ख़ास कर लेना यह दिल और ज़मीर की पाकीज़गी है। पाकीज़गी और तहारत के ये चौतरफ़ा मरहले इमाम ग़ज़ाली ने बहुत तफ़सील से अपनी कई किताबों में बयान किए हैं। यानी—
- जिस्म औ लिबास को ज़ाहिरी नापाकियों से बचाना और पाक करना।
- जिस्म को अल्लाह तआला की नाफ़रमानी से बचाना
- दिल और रूह को नैतिक बुराइयों से पाक करना
- दिल और ज़मीर को अल्लाह के अलावा दूसरों का केन्द्र बनने से बचाना और सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ासकर लेना।
जब इंसान ज़ाहिरी और आन्तरिक रूप से पाकीज़गी अपना लेता है तो फिर वह अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाता है। शरीअत के आदेशों में सबसे सर्वप्रथम आदेश, और उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य अल्लाह और बंदे के दरमियान सम्बन्ध को मज़बूत बनाना है। यों तो सम्बन्ध की यह मज़बूती शरीअत के सारे आदेशों का उद्देश्य है और शरीअत के हर आदेश पर अमल करने से यह सम्बन्ध मज़बूत होता है, बशर्तेकि अल्लाह के आदेशों के पालन का संकल्प करते हुए और अल्लाह की प्रसन्नता की प्राप्ति की ख़ातिर शरीअत के आदेशों पर कार्यान्वयन किया जाए। लेकिन विशेष रूप से जिन कर्मों और आदेशों को इबादात कहा जाता है उनका तो सर्वप्रथम उद्देश्य यही है। इंसानों को इबादत के लिए आमादा करने की ख़ातिर और यह बताने की ख़ातिर कि जब इंसान अल्लाह के सामने नतमस्तक होता है और अल्लाह की इबादत करता है तो दरअस्ल वह स्वयं को सृष्टि की उन सभी शक्तियों का हमसफ़र बना लेता है जो अल्लाह के आदेश के अधीन हैं और सृष्टि की इस व्यवस्था में अल्लाह के आदेशों का पालन कर रही हैं।
यह सृष्टि पूरी-की-पूरी, ये तमाम ग्रह-उपग्रह, अन्तरिक्ष के तमाम पिंड अल्लाह के आदेशों का पालन कर रहे हैं और अल्लाह के आदेशों से कण भर भी विमुख नहीं होते, “आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वे सब अल्लाह के सामने नतमस्तक है, अपनी इच्छा से भी और बिना इच्छा के भी।” (क़ुरआन, 13:15) वह मजबूर है कि अल्लाह के आदेश का पालन करे और अल्लाह ने जिस तरह से उसको अपने आदेश के अधीन किया है उस आदेश पर कार्यरत रहे। हर चीज़ अपनी स्थिति या अपनी ज़बान से या अपने रवैये से अल्लाह का गुणगान करने में लगी है। लेकिन अगर इंसान इबादत करते हुए यह एहसास रखे कि वह सृष्टि की इन तमाम शक्तियों के साथ सफ़र कर रहा है जो अल्लाह के सामने चल रही हैं तो उसकी इबादत में एक नई सार्थकता और एक नई शान पैदा हो जाती है। इस पाकीज़गी और ज़ाहिरी तहारत के आधार पर इस्लामी शरीअत इंसानों की ज़िन्दगी को संगठित और क़ायम करना चाहती है। एक बार आन्तरिक और बाह्य पाकी प्राप्त करने के बाद जब इंसान शरीअत के आदेशों पर अमल करता है तो उसके नतीजे में एक नई जीवन शैली सामने आती है। इस नए ढंग से एक ऐसी आध्यात्मिक सभ्यता क़ायम होती है, एक ऐसा पाकीज़ा समाज उभरता है जिसके बारे में यह उम्मीद की जाती है कि उसका आधार पाकीज़गी, कर्मों की सफ़ाई, दिलों की सफ़ाई और अल्लाह के साथ सम्बन्ध पर होता है। यह है वह आध्यात्मिक आधार जिसपर शरीअत के आदेश दिए गए।
यह सवाल इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) के दरमियान शुरू से चर्चा में रहा है कि क्या इस्लामी शरीअत में दिए जानेवाले आदेश यानी अवामिरो-नवाही (आदेश और निषेधाज्ञाओं) के कोई उद्देश्य और लक्ष्य हैं या इन सबका उद्देश्य मात्र इंसानों की परीक्षा है। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ कि पवित्र क़ुरआन में कई जगह यह बताया गया है कि हमने मृत्यु एवं जीवन का यह सारा सिलसिला इसलिए पैदा किया है कि हम परीक्षा लेकर यह दिखाना चाहते हैं कि कौन सदाचारी है और कौन दुराचारी है। अल्लाह तआला परीक्षा लेना चाहता है, एक इम्तिहान करना चाहता है जिससे तमाम प्राणियों के सामने यह स्पष्ट हो जाए कि इंसानों में सदाचारी कौन है और दुराचारी कौन?
कुछ इस्लामी चिन्तकों ने यह राय ज़ाहिर की कि चूँकि मूल उद्देश्य सदाचारियों और दुराचारियों का निर्धारण है इसलिए हर-हर आदेश में अपने आपमें किसी तत्त्वदर्शिता या उद्देश्य का पाया जाना ज़रूरी नहीं। कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है कि अगर कोई मालिक अपने नौकरों या ग़ुलामों की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहे या कार्यकुशलता को जाँचना चाहे और इसके लिए कोई ज़िम्मेदारी उनके सिपुर्द कर दे तो यह ज़रूरी नहीं कि ख़ुद उस ज़िम्मेदारी या उस काम में भी अपनी जगह कोई तत्त्वदर्शिता या उद्देश्य मौजूद हो, इस ज़िम्मेदारी या प्रस्तुत कार्य का यह उद्देश्य काफ़ी है कि उसके द्वारा नौकरों या सेवकों की ईमानदारी जाँचना अभीष्ट है। यही कैफ़ियत उन लोगों की राय में शरीअत के आदेशों की भी है। इसलिए शरीअत के आंशिक आदेशों में कोई तत्त्वदर्शिता या निहितार्थ तलाश करना इन लोगों के ख़याल में ग़ैर-ज़रूरी है। कुछ और विद्वान जिनपर तौहीद (एकेश्वरवाद) और अल्लाह के सर्वशक्तिमान होने की धारणा बहुत अधिक प्रभावी थी। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर अल्लाह तआला के आदेशों को निहितार्थों का पाबंद क़रार दिया जाए या निहितार्थों के आधार पर घटित होनेवाला क़रार दिया जाए तो यह अल्लाह तआला की असीमित सामर्थ्य के ख़िलाफ़ है। किसी निहितार्थ या उद्देश्य का पाबन्द तो इंसान होता है, या दूसरे प्राणी होते हैं जिनकी क्षमताएँ सीमित हैं, अधिकार सीमित हैं, शक्ति सीमित है, इसलिए वे किसी-न-किसी लाभ या उद्देश्य की ख़ातिर कोई काम करते हैं। वह सत्ता जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके अधिकार और शक्ति की कोई हद न हो उसको किसी नियम या अनुशासन का पाबन्द करना या समझना उचित नहीं।
इन कुछ व्यक्तिगत या बहुत विरली रायों के साथ-साथ विद्वानों की अधिक संख्या की राय यह रही है कि अल्लाह तआला के तमाम आदेश निहितार्थ और उद्देश्यों पर आधारित हैं। अल्लाह तआला की सत्ता पूर्ण तत्त्वदर्शी है और किसी तत्त्वदर्शी का कर्म तत्त्वदर्शिता और बुद्धिमत्ता से ख़ाली नहीं होता। जो सत्ता तमाम बुद्धिमत्ताओं और तत्त्वदर्शिताओं का मुख्य स्रोत है, उसके फ़ैसले और उसके आदेश तत्त्वदर्शिताओं से कैसे ख़ाली हो सकते हैं। पवित्र क़ुरआन को अगर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि पवित्र क़ुरआन जहाँ क़ानून है वहाँ वह तत्त्वदर्शिता भी है, शुभसूचना देनेवाला और चेतावनी देनेवाला भी है और उन तमाम विशिष्टताओं को समेटे हुए है जो पूर्व आसमानी ग्रन्थों में रखी गईं। तौरात का मौलिक गुण शिक्षा और सावधान करना मालूम होता है। तौरात में क़ानून के आदेश दिए गए और यहूदियों को उनके अंजाम से डराया गया। मानो सावधान करने का गुण तौरात में नुमायाँ तौर पर सामने आता है। इसके मुक़ाबले में इंजील क़ानूने-इलाही की तत्त्वदर्शिता पर ज़्यादा ज़ोर देती है। उसने उच्च नैतिक सिद्धान्तों पर रौशनी डाली है और आसमानी बादशाहत की शुभसूचनाएँ दी हैं। इस दृष्टि से इंजील शुभसूचना देने का कर्त्तव्य अंजाम देती है। पवित्र क़ुरआन में चेतावनी भी है और शुभसूचना देना भी है। पवित्र क़ुरआन में क़ानून भी है और क़ानून की तत्त्वदर्शिता भी है। पवित्र क़ुरआन में तौरात की तरह के सख़्त क़ानून भी हैं। कुछ क़ानून बिलकुल उसी तरह हैं जिस तरह तौरात में आए थे। इसके साथ-साथ उन क़ानूनों की उच्च नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वदर्शिता और उद्देश्य को भी बयान किया गया है। इसलिए यह कहना कि पवित्र क़ुरआन के आदेशों में कोई तत्त्वदर्शिता या निहितार्थ नहीं है यह शरीअत को न समझने की वजह से है।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इस किताब में जिसका अभी ज़िक्र हुआ, यानी हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा के मुक़द्दमे (प्राक्कथन) में बहुत विस्तार से यह बयान किया है कि यह समझना सही नहीं है कि शरीअत के आदेशों में कोई निहितार्थ या तत्त्वदर्शिताएँ नहीं हैं। उन्होंने मिसालें देकर एक-एक करके यह बताया है कि यह ख़याल बिलकुल निराधार और ग़लत है, मुतक़द्दिमीन (पहले ज़माने के फ़ुक़हा) के ज़माने से ही कुछ लोगों ने पवित्र क़ुरआन और शरीअत के आदेशों में तत्त्वदर्शिता और निहितार्थों की तलाश को अपनी दिलचस्पी का विशेष मैदान क़रार दिया। इन विद्वानों में हकीम तिरमिज़ी, इमाम क़फ़्फ़ाल शाशी, इमाम ग़ज़ाली के महान उस्ताद इमामुल-हरमैन अब्दुल-मलिक अलजवैनी और ख़ुद इमाम ग़ज़ाली बहुत नुमायाँ स्थान रखते हैं। इन लोगों ने शरीअत के उद्देश्यों की तलाश और सभ्यता और संकलन को अपने ज्ञानपरक कामों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा क़रार दिया है और अपने लेखों में शरीअत के उद्देश्यों के दर्शन को संकलित करने की कोशिश की है। इमामुल-हरमैन ने किताबुल-बुरहान में, इमाम ग़ज़ाली ने किताब ‘अल-मुस्तसफ़ा’ में और दूसरे लेखों में शरीअत के उद्देश्यों पर बहुत विस्तार से इसपर रौशनी डाली है। इन लोगों के बाद सुल्तानुल-उलमा अल्लामा इज़ुद्दीन-बिन-अब्दुस्सलाम अस-सुलमी, उनके शागिर्द इमाम क़राफ़ी, उनके शागिर्द इमाम शातबी का काम इस मैदान में बहुत नुमायां और ऐतिहासिक है। दूसरी तरफ़ अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) और उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने-क़य्यिम (रह॰) हैं, इन लोगों ने कुतुबख़ाने (पुस्तकालय) इसपर तैयार कर दिए कि शरीअत के आदेशों के उद्देश्य क्या हैं, तत्त्वदर्शिताएँ और निहितात क्या हैं।
शाह वलीउल्लाह साहब ने इसको ‘इल्मे-इसरारे-दीन’ (दीन के रहस्यों का इल्म) का नाम दिया है। मुतक़द्दिमीन (पहले के विद्वानों) ने इसको शरीअत के उद्देश्य का नाम दिया है। किसी ने इसको तत्त्वदर्शिता का नाम दिया किसी ने इसको मुहासिने-शरीअत का नाम दिया, नाम विभिन्न रहे हों, लेकिन उद्देश्य और लिखी बातें सब के यहाँ समान ही हैं।
शाह साहब ने इसको इस्लामी ज्ञान-विज्ञान की बुनियाद क़रार दिया है। सच तो यह है कि इन सब फ़िक़्ह के इमामों में से जिनका मैंने नाम लिया है इमाम शातबी इस कला में इमामत का दर्जा रखते हैं और शरीअत के इल्म के उद्देश्यों को यानी शरीअत के आदेशों में तत्त्वदर्शिता और इल्म की तलाश को उन्होंने एक अत्यन्त संगठित, क्रमबद्ध, तार्किक और मुरत्तिब ज्ञान का रूप दे दिया है।
✩✩✩
Recent posts
-
नैतिकता और नैतिक संस्कृति (लेक्चर # 4)
31 August 2025 -
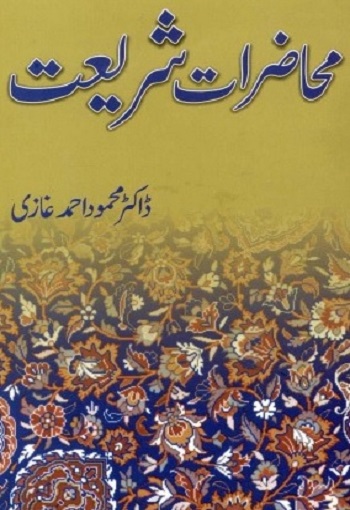
मुसलमान और मुस्लिम समाज (शरीअत : लेक्चर # 3)
28 August 2025 -
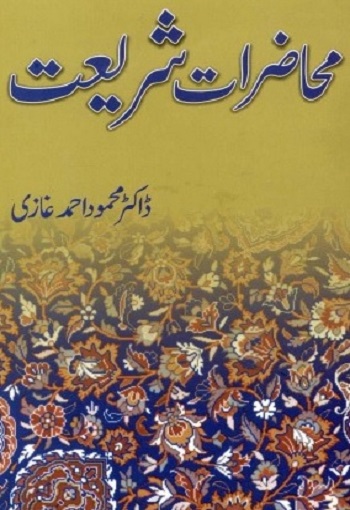
इस्लामी शरीअत : विशिष्टताएँ, उद्देश्य और तत्त्वदर्शिता (शरीअत: लेक्चर #2)
17 August 2025 -
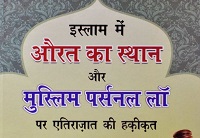
इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एतिराज़ात की हक़ीक़त
22 March 2024 -

इस्लामी शरीअ़त
21 March 2024 -

परदा (इस्लाम में परदा और औरत की हैसियत)
21 March 2024