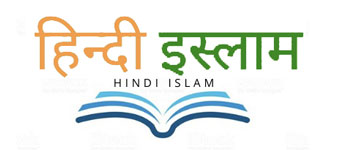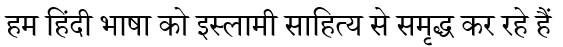अक़ीदा और ईमानियात - शरई व्यवस्था का पहला आधार (शरीअत : लेक्चर# 9)
-
शरीअत
- at 17 November 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
अक़ीदे और ईमानियात अर्थात् आस्था एवं धार्मिक अवधारणाओं की समस्या दुनिया के हर धर्म के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और मौलिक समस्या रही है। संसार के तमाम धर्मों में आस्था सम्बन्धित एक ऐसी व्यवस्था हमेशा एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में शामिल रही है जो उस धर्म की मौलिक धारणाओं, उस धर्म के मौलिक ढाँचे के और उसकी शिक्षाओं के फ़ाइनल और आख़िरी आधार का निर्धारण करती रही है। यह बात कि इस मूल धारणा का अपना आधार क्या हो, यह अक़ीदे (धार्मिक अवधारणा) से भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण समस्या है। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि धर्म के इतिहास में अक़ीदे का आधार और बुनियाद कभी भी सर्वसम्मत नहीं रही है।
फिर भी संसार के विभिन्न धर्मों में पाए जानेवाली आस्था-व्यवस्था का जायज़ा लिया जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है, और वह यह कि उनमें से अधिकांश धर्मों की व्यवस्था किसी बौद्धिक या बुद्धिसंगत आधार पर क़ायम नहीं है। आज दुनिया की अति विकसित क़ौमें जिस धर्म की अनुयायी हैं और उस धर्म के बारे में उदासीनता के ज़ाहिरी दावों के बावजूद उनके यहाँ ख़ासे पक्षपात और सख़्ती का प्रदर्शन उनकी नीतियों में पाया जाता है। उसके आधार के बौद्धिक और तार्किक रूप से स्वीकार्य होने के बारे में वे स्वयं भी असमंजस का शिकार हैं। पश्चिमी क़ौमें जिस धर्म की अनुयायी हैं उस धर्म की धारणाओं का आधार क्या है, इसके बारे में ख़ुद वहाँ के विद्वानों के ज़ेहन साफ़ नहीं हैं, न वे पूर्ण रूप से बुद्धि को आधार क़रार देते हैं और न केवल वह्य (ईश-प्रकाशना) या धार्मिक निर्देशों को। उनके यहाँ अक़ीदे का आधार सुने-सुनाए क़िस्सों या किवदंतियों पर है। वे कुछ मामलों को (उनके बौद्धिक या अबौद्धिक, बोधगम्य या न समझने योग्य होने से परे) बनाए हुए सिद्धान्त के तौर पर मान लेते हैं जिनको डोगमा के नाम से याद किया जाता है। यही Dogma के सिद्धान्त उनके अक़ीदे (धार्मिक अवधारणाएँ) कहलाते हैं।
यही कारण है कि दुनिया के बहुत-से धर्मों में उनके न समझ में आनेवाले अक़ीदों के आधार पर एक ऐसी कला अस्तित्व में आई जिससे मुसलमान हमेशा अपरिचित रहे हैं और हर समझदार और सभ्य इंसान उससे अनभिज्ञ रहना पसन्द करता है। यह वह चीज़ है जिसको mythology या देवमालाई ज्ञान कहा जा सकता है। ‘सनमियात’ या बुतों की कहानियाँ और देवताओं की पवित्र दंत-कथाएँ जिनका कोई ज्ञानपरक और ऐतिहासिक आधार न हो। यह अतार्किक और इतिहास से परे देवमालाई ज्ञान दुनिया के हर धर्म में पाया जाता है, इसलिए कि जिन आस्थाओं या जिन पहेलियों पर आधारित अक़ीदों को वे अपने धर्म का आधार मानते हैं उन अक़ीदों की अनिवार्य अपेक्षा है कि इस तरह की किवदंतियाँ और क़िस्से-कहानियाँ जन्म लें। हमारे आस-पास में जो क़ौम बस्ती है, वह जिस धारणा-व्यवस्था की अनुयायी है, उसका ज़ेहन इस तरह की किवदंतियों और देवमालाई कहानियों को जन्म देने में बहुत आगे है। उनके यहाँ इतने हज़ारों, लाखों क़िस्से उनके धार्मिक क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुए हैं और अस्तित्व में आए हैं कि वे अब उनकी आस्था का हिस्सा हैं। अगर आस्था का हिस्सा नहीं हैं तो उनके धार्मिक लोकाचार (ethos) का हिस्सा ज़रूर हैं। उनकी अपनी धारणाओं एवं विचारधाराओं की झलक उनमें पाई जाती है।
कुछ पश्चिमी भाषाओं में अक़ीदे के लिए dogma का शब्द चल पड़ा है। डोगमा से मुराद एक ऐसा गढ़ा हुआ विचार या एक ऐसा रहस्यमय विचार है जिसको बिना किसी बौद्धिक या तार्किक प्रमाण के माने बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। एक गढ़े हुए सिद्धान्त के तौर पर इस कपोल-कल्पित विचार को पहले क़दम पर ही आप स्वीकार कर लें। चाहे वह वास्तविकता में कोई बुद्धिसंगत और समझ में आनेवाली बात हो या न हो, लेकिन आप उसे बिना किसी बौद्धिक व्याख्या और स्पष्टीकरण के स्वीकार कर लें। इस रहस्यमय विचार को जिसके आधार पर आगे चलकर बहुत-से मामलों का दारोमदार हो स्वीकार कर लेना dogma कहलाता है। यही वह चीज़ है जिसको ग़लती से अक़ीदे का नाम दे दिया जाता है। इस्लाम में (अल्लाह का शुक्र है कि) न कोई dogma है, न कोई माइथालॉजी और न ही किवदंतियों की तरह की कोई दास्तानें। इस्लाम का आधार एक ऐसी वास्तविकता पर है जो हर सद्बुद्धि रखनेवाला इंसान स्वीकार करता है और न केवल आज, बल्कि निकट अतीत, सुदूर अतीत यहाँ तक कि मानव इतिहास के हर दौर के सद्बुद्धि रखनेवाले इंसान इसको स्वीकार करते रहे हैं। बहरहाल यह वह चीज़ है जिसको दुनिया के विभिन्न धर्मों में dogma के नाम से याद किया जाता है।
इसके विपरीत मुसलमान जिस चीज़ को अक़ीदा कहते हैं वह मौलिक महत्त्व रखनेवाली एक बहुत अर्थपूर्ण वास्तविकता है। ‘अक़ीदा’ का शब्द जो ‘अक़्द’ से निकला है इसका अर्थ गाँठ बाँधना है। दो रस्सियों में गाँठ बाँधकर एक रस्सी बना देने को ‘अक़्द’ कहते हैं। इससे दीवानी समझौते का अर्थ भी निकलता है। दो इंसानों में क्रय-विक्रय, लेन-देन या किसी और मामले के सिलसिले में जो समझौता होता है वह ‘अक़्द’ कहलाता है। ‘अक़्दे-निकाह’ को भी ‘अक़्द’ इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो इंसान अपने-आपको एक अनुबन्ध के द्वारा एक नए रिश्ते या गाँठ में बाँध लेते हैं। ‘उक़्दा’ उस पेचीदा समस्या को कहते हैं, जिसे खोला (सुलझाया) न जा सके। ऐसी गाँठ या गुत्थी जो खोली न जा सके, वह अरबी भाषा में ‘उक़्दा’ कहलाती है। यों ‘अक़ीदे’ से मुराद है वह लम्बी रस्सी जो बहुत-सी रस्सियों को बाँधकर बनाई गई हो और रास्ते को निर्धारित करने के लिए रेगिस्तान में बाँध दी गई हो। ‘अक़ीदे’ का एक मतलब वह रस्सी भी है जो एक बड़े लम्बे-चौड़े मैदान में या किसी सुनसान रेगिस्तान में, रास्ते के निर्धारण के लिए बाँध दी जाए।
‘अक़ीदे’ का अर्थ किसी के ज़ेहन को बाँध देना या पाबन्द कर देना नहीं है। ‘अक़ीदे’ का अर्थ मानसिक आज़ादी को समाप्त कर देना भी नहीं है, ‘अक़ीदे’ का अर्थ मानव-बुद्धि को काम करने से रोकना भी नहीं है, बल्कि ‘अक़ीदे’ का अर्थ विचारों के इस असीमित जंगल में, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है, मानव-बुद्धि का सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। मानव-बुद्धि किसी भी तरफ़ जा सकती है। मानव बुद्धि सौ भेस बना सकती है, वह कोई भी रास्ता अपना सकती है। इस वीरान रेगिस्तान में मानव-बुद्धि को सकारात्मक रास्ते पर बनाए रखने के लिए और सकारात्मक रास्ते पर चलने और सफ़र जारी रखने में आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह तआला ने जगह-जगह मील के पत्थरों की निशानदेही कर दी है, मंज़िल के निशानात लगा दिए हैं कि अगर इस रास्ते पर चलकर जाओगे तो गन्तव्य स्थान तक पहुँच जाओगे।
यही वे सफ़र के निशानात हैं जिसको इस्लामी विचारधारा में ‘अक़ीदा’ कहा जाता है। ‘अक़ीदे’ में उन मौलिक सवालों का जवाब दिया गया है जो हर इंसान पूछता है और जो हर इंसान के दिल में पैदा होते हैं। एक छोटे-से-छोटा बच्चा भी, जिसकी उम्र कुछ साल से अधिक न हो, कुछ ऐसे सवालात पूछता है जिनका अक़ीदे से गहरा सम्बन्ध होता है। वह पूछता है कि वह कहाँ से आया है? और आख़िरकार उसे कहाँ जाना है? यहाँ उसकी ज़िम्मेदारी क्या है और जिस दुनिया में वह ज़िन्दगी गुज़ार रहा है उस दुनिया से उसका सम्बन्ध और सम्पर्क किस प्रकार का है? अगर इन सवालों के जवाबों के बारे में ग़ौर किया जाए तो हमारे सामने तीन सम्भावित स्थितियाँ आती हैं, और उनके तीन परिणाम भी सामने आते हैं।
पहली सम्भावित स्थिति तो यह है कि अल्लाह तआला ने ही उनमें से किसी सवाल का जवाब न दिया होता, अक़ीदे के बारे में कोई बात न बताई होती और हर चीज़ आरम्भ से लेकर अन्त तक पूरी तरह मानव-बुद्धि पर छोड़ दी होती, यों इन तमाम महत्त्वपूर्ण और मौलिक सवालों के जवाब मानव-बुद्धि ख़ुद ही देती।
दूसरा सम्भावित रास्ता यह था कि जितने सवालात इंसान के ज़ेहन में अतीत में उभरे हैं या आज पाए जाते हैं या भविष्य में जन्म लेंगे, उन सबका जवाब विस्तार से वह्य (ईश-प्रकाशना) के द्वारा देकर किताबों में संकलित और क्रमबद्ध करा दिया जाता।
ज़रा-सा ग़ौर करने से अन्दाज़ा हो जाता है कि ये दोनों सम्भावनाएँ अव्यावहारिक थीं। पहली सम्भावना इसलिए अव्यावहारिक थी कि इंसानों की अक़्लें अलग-अलग हैं। इंसानों के अन्दाज़े और सोचने-समझने के अन्दाज़ विभिन्न हैं। जितने इंसान हैं उतनी ही अक़्लें भी हैं। अत: जितने इंसान दुनिया में होते, उतने ही अक़ीदे, उतने ही जवाब अस्तित्व में आते, बल्कि दस इंसानों के ज़ेहन ग्यारह जवाब सोचते। हम सब देखते रहते हैं कि कभी-कभी महत्त्वपूर्ण मामलों के बारे में एक इंसान रोज़ एक नया जवाब लेकर आता है, यों दुनिया ऐसी भूल-भुलैयों का शिकार हो जाती कि किसी सवाल का स्पष्ट जवाब इंसान के सामने न आता। जैसा कि कुछ मामलों में पश्चिमी दुनिया में हम देखते हैं। आए दिन का अनुभव है कि सामूहिक ज्ञान और मानव ज्ञान के मामले में रोज़ाना कोई-न-कोई नया नज़रिया, नई धारणा सामने आती है और इस धारणा के आधार पर नए सिरे से ज्ञान-विज्ञान के संकलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तमाम मामलों को इस विशेष दृष्टिकोण से देखने का चलन शुरू हो जाता है। अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पाती कि कोई और तस्वीर सामने आ जाती है। यहाँ तक कि कोई तीसरी, चौथी, पाँचवीं, बल्कि नए से नई धारणा सामने आती रहती है। जिसका परिणाम यह है कि सोच में कोई निरन्तरता क़ायम नहीं रहती। सोच की कोमल नौका को प्रवाह प्राप्त नहीं होने पाता। इसलिए इस सम्भावना को अल्लाह तआला की असीम दयालुता और नियति ने पसन्द नहीं किया।
दूसरी सम्भावना यह थी कि इंसानों के ज़ेहन में आनेवाले तमाम सम्भावित प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिए जाते। तमाम सम्भावित प्रश्न उतने ही हो सकते थे जितने इंसान हैं। इस सम्भावना को अपनाए जाने की स्थिति में शायद इतनी किताबें लिखने की ज़रूरत पेश आती जितनी आज दुनिया के पुस्तकालयों में मिलाकर पाई जाती हैं। ज़ाहिर है कि यह भी कोई व्यावहारिक बात नहीं। न तो इंसानों के लिए पुस्तकों के इस सारे भंडार से लाभान्वित होना आसान होता और न ही कोई स्पष्ट बात सामने आती।
इसलिए अल्लाह की तत्त्वदर्शिता और नियति ने एक तीसरा रास्ता चुना। वह तीसरा रास्ता यह था कि ऐसे अति महत्त्वपूर्ण और मौलिक प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर सारगर्भित ढंग से उपलब्ध कर दिया जाए जो हर इंसान के ज़ेहन में पैदा होते हैं, वे सवालात जो हर ज़माने का इंसान पूछेगा और जो हर ज़माने के सन्दर्भ में सार्थकता रखते हों। उन सवालों का जवाब स्पष्ट और दोटूक अन्दाज़ में दे दिया जाए और ऐसे मार्गदर्शक चिह्न निर्धारित कर दिए जाएँ जिनसे लाभ उठाते हुए मानव-बुद्धि ख़ुद-ब-ख़ुद शेष प्रश्नों का उत्तर देती चली जाए। जब भी इन मौलिक आधारों के हवाले से कोई नया सवाल पैदा हो तो मंज़िल के उन निशानों की सहायता से नई समस्याओं का ऐसा तर्कसंगत और सटीक उत्तर सामने आ जाए जो शरीअत की दी हुई मौलिक बुनियादों के अनुसार हो और सद्बुद्धि रखनेवाले इंसान की बुद्धि के लिए स्वीकार्य क़रार पाए। इस कार्य-नीति से मानव-बुद्धि को पूर्ण और प्रभावकारी रूप से अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी मिलता है और उसको वह्य (ईश-प्रकाशना) और ईश्वरीय मार्गदर्शन की रौशनी भी प्राप्त रहती है। इसके विपरीत अगर दूसरी सम्भावना अपनाई गई होती तो मानव-बुद्धि एक निष्क्रिय अंग बनकर रह जाती।
अगर पहली सम्भावना अपनाई गई होती तो यह मानव-बुद्धि के लिए असहनीय बोझ बन जाता और ऐसे-ऐसे मामलों का बोझ उसपर पड़ जाता जिनको सहन करने की उसमें क्षमता न थी। मानव-बुद्धि एक विशेष परिवेश और एक विशेष उद्देश्य की ख़ातिर बनाई गई है। इसके लिए सम्भवतः मौलाना रूमी ने एक जगह बड़ी सूक्ष्म उपमा दी है। वे कहते हैं कि बुद्धि एक तराज़ू है जो सत्य-असत्य का फ़ैसला कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि बुद्धि एक तराज़ू है। लेकिन एक तराज़ू तो वह होता है जो मोती तौलने के काम आता है। एक तराज़ू वह होता है जो बड़े-बड़े बोझ तौलता है। अगर बड़े बोझ और माल ढोनेवाले जहाज़ तौलनेवाले तराज़ू से मोती तौलने का काम लिया जाए तो यह उसका सही उपयोग नहीं होगा। इसी तरह अगर मोती तौलनेवाले तराज़ू पर भारी बोझ लाद दिया जाए तो तराज़ू भी सलामत नहीं रहेगा और शायद तौलनेवाले भी ख़त्म हो जाएँगे।
यही कैफ़ियत मानव-बुद्धि और अल्लाह द्वारा अवतरित वह्य की है। वह्य उन बड़े-बड़े सवालों का जवाब दे रही है जिनके उत्तर मालूम करना मानव-बुद्धि के बस की बात नहीं। इसके बाद उन मौलिक प्रश्नों की रौशनी में मानव-बुद्धि तुलनात्मक रूप से छोटे और बुद्धि, अवलोकन और अनुभव में आनेवाली समस्याओं का जवाब दे सकती है। इस प्रक्रिया में बुद्धि के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह द्वारा अवतरित वह्य और मार्गदर्शक पुस्तक मौजूद है। यह भूमिका है जो शरीअत का वह हिस्सा निभाता है जिसको हम अक़ीदा और ईमानियात कहते हैं।
सम्भव है कि यहाँ किसी के ज़ेहन में यह सवाल पैदा हो कि यह बात कि इंसान की भूमिका इस सृष्टि में क्या है? इसका जवाब तो दर्शन ने भी दिया है। इसका जवाब मनुष्य जाति का विज्ञान अर्थात् Anthropology ने भी दिया है। इसका जवाब इतिहास भी देने की कोशिशें करता रहा है, और भी बहुत सारे ज्ञान-विज्ञान हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिशें की हैं। क्या इन तमाम प्रयासों से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता जो अक़ीदे से पूरा किया जा रहा है।
ज़रा-सा ग़ौर करने से अन्दाज़ा हो जाता है कि पवित्र क़ुरआन और उन तमाम ज्ञान एवं कलाओं में एक मौलिक अन्तर है। वह यह है कि पवित्र क़ुरआन जब इन सवालों का जवाब देता है तो उसमें दो मौलिक और विशेष गुण पाए जाते हैं जो शेष प्रयासों में नहीं पाए जाते। एक मौलिक गुण तो यह है कि पवित्र क़ुरआन की शैली और सन्देश सरासर व्यावहारिक है, केवल बौद्धिक समस्याएँ और बहसें यानी abstract मामले पवित्र क़ुरआन की दिलचस्पी के मामले नहीं हैं। इसलिए कि यह एक व्यावहारिक पुस्तक और विशुद्ध मार्गदर्शक ग्रन्थ है। फिर पवित्र क़ुरआन कुछ दार्शनिकों फ़ाराबी और इब्ने-सीना जैसे चिन्तकों के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आप जैसे हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है। इसलिए अगर पवित्र क़ुरआन केवल उन समस्याओं से बहस करता जो फ़ाराबी और इब्ने-सीना जैसे दार्शनिकों या मात्र ग़ज़ाली और राज़ी जैसे चिन्तकों ही की दिलचस्पी के हैं तो फिर फ़ाराबी और इब्ने-सीना ही क़ुरआन को पढ़ा करते, ग़ज़ाली और राज़ी ही क़ुरआन से लाभान्वित होते, शेष कोई इंसान पवित्र क़ुरआन को न पढ़ा करता। इसलिए पवित्र क़ुरआन ने अपनी दिलचस्पी व्यावहारिक और वास्तविक समस्याओं तक सीमित रखी।
दूसरा विशेष गुण यह है कि अधिकांश समाज शास्त्र और मानवीय ज्ञान-विज्ञान का ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि इंसान के अतीत के बारे में खोज लगाई जाए कि इंसान आया कहाँ से है और इंसान का आरम्भ कैसे हुआ? इसके बारे में हज़ारों विचारधाराएँ और धारणाएँ पेश की गईं। हकीम अफ़लातून से भी पहले से लोग इसपर विचार करते चले आ रहे हैं और नए-नए प्रश्न उठाकर उनके नए-नए उत्तर दे रहे हैं। पवित्र क़ुरआन ने भी इंसान के आरम्भ की समस्या पर रौशनी डाली है, लेकिन मानव प्रयासों के विपरीत पवित्र क़ुरआन ने ज़्यादा ज़ोर अतीत पर नहीं दिया, पवित्र क़ुरआन का अस्ल ज़ोर भविष्य पर है। इसलिए कि भविष्य का निर्माण और गठन इंसानों के अधिकार में है। अतीत का निर्माण एवं गठन अब इंसानों के अधिकार में नहीं है। अगर कोई इंसान यह चाहे कि अपने अतीत को आज बना ले तो वह ऐसा नहीं कर सकता। अतीत को बनाना या बिगाड़ना अब किसी के वश में नहीं है। जो कुछ होना था वह हो चुका। अब केवल भविष्य इंसान के वश में है। भविष्य को बनाने या बिगाड़ने का अधिकार अब भी इंसान के हाथ में है। इसलिए व्यावहारिक मार्गदर्शक पुस्तक होने की हैसियत में पवित्र क़ुरआन की दिलचस्पी भविष्य से है।
इस अन्तर को अल्लामा इक़बाल ने बड़े सूक्ष्म और गूढ़ शैली में बयान किया है। उन्होंने इब्ने-सीना और रूमी इन दोनों को दो विभिन्न आयामों का प्रवक्ता क़रार दिया है। इब्ने-सीना के बारे में अल्लामा कहते हैं कि वह पूछता है कि मैं आया कहाँ से हूँ। इसके विपरीत रूमी पूछते हैं कि जाऊँ किधर को मैं? रूमी का अस्ल सवाल यह है कि मुझे जाना कहाँ है? इब्ने-सीना की दिलचस्पी मूल रूप से यह है कि मैं आया कहाँ से हूँ। यह अन्तर है क़ुरआन की approach और शेष मानवीय और सामाजिक ज्ञान के approach में।
सारांश यह कि अक़ीदों के मामले में पवित्र क़ुरआन ने जिन मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया है वे तीन बड़े शीर्षकों के तहत बयान किए जा सकते हैं। शेष सभी प्रश्न गौण और द्वितीय दर्जे के हैं और इन्हीं तीन मौलिक शीर्षकों से सम्बन्धित हैं। अत: जो मूल आधार और अक़ीदे हैं वे तीन हैं। एक यह कि यह सृष्टि किसी संयोग या दुर्घटना के परिणामस्वरूप पैदा नहीं हुई, बल्कि यह एक तत्त्वदर्शी ईश्वर, सर्वशक्तिमान, आदिकालीन, सर्वज्ञ की सोचे-समझी योजना का परिणाम है। अल्लाह तआला तत्त्वदर्शी भी है, उसका हर फ़ैसला पूर्ण तत्त्वदर्शिता और बुद्धिमानी पर आधारित होता है। इसलिए सृष्टि की रचना पूरी बुद्धिमत्ता और तत्त्वदर्शिता के साथ की गई। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तआला ने इस सृष्टि को किसी उद्देश्य के बिना पैदा नहीं किया। इस सृष्टि का एक निर्धारित उद्देश्य है जिसकी ख़ातिर यह पैदा की गई है। जब तक उद्देश्य के बारे में इंसान का ज़ेहन स्पष्ट न हो, इंसान ज़िन्दगी के बारे में अपना रवैया तय नहीं कर सकता। अपना रवैया और तर्ज़े-अमल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको यह मालूम हो कि आप जहाँ भेजे गए हैं वहाँ किस काम के लिए भेजे गए हैं और कितने दिन के लिए भेजे गए
हैं।
अगर आपको हवाई जहाज़ का टिकट देकर किसी नई और अजनबी जगह भेजा जाए और यह बताया जाए कि वहाँ आपको अमुक जगह नौकरी करनी है। उसकी ये और ये शर्तें होंगी। आपकी वहाँ अमुक और अमुक ज़िम्मेदारियाँ होंगी और ये-ये काम आपको करने होंगे, तो आपका रवैया वहाँ पहुँचने पर और होगा, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति भी आपके साथ जा रहा है जिसको कहीं से बहुत ज़्यादा दौलत मुफ़्त हाथ आ गई है और वह बिना किसी उद्देश्य के वहाँ पहुँचा है और अपने घरवालों से छिपकर वह इस दौलत को मात्र अय्याशी में उड़ाना चाहता है। उस व्यक्ति के रवैये में और आपके रवैये में बहुत अन्तर होगा। एक और व्यक्ति है जिसके पास दौलत नहीं है, उसे भविष्य का भी ज्ञान नहीं है, हालात से परेशान है, रोज़गार भी नहीं है। वह यह समझते हुए कि इस तरह बाहर जाकर नौकरी मिल जाती है, वह किसी-न-किसी तरह से आपके साथ वहाँ पहुँचने में सफल हो जाता है। अब इन तीनों व्यक्ति के मानसिक रवैये, स्वभाव और तर्ज़े-अमल में बहुत स्पष्ट अन्तर होगा। इससे पता चला कि सफ़र के उद्देश्य से सफ़र के दौरान रवैये का गठन होता है।
इसलिए अक़ीदों के मामले में पवित्र क़ुरआन सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर देता है कि हर इंसान को हर समय यह याद रहे कि उसको यहाँ दुनिया में भेजने का उद्देश्य क्या है? अगर यहाँ भेजनेवाला इनसान का पैदा करनेवाला और उसका मालिक ख़ुदा है, सर्वज्ञानी और तत्त्वदर्शी ख़ुदा है तो वह यह भी जानता है कि उसने इंसान को किस उद्देश्य के लिए भेजा है और यह भी जानता है कि वह उद्देश्य क्या है? अभी जिन धर्मों का मैंने उदाहरण दिया उनमें सृष्टि के जन्म का कारण और तत्त्वदर्शिता के बारे में जो अक़ीदा पाया जाता है वह बड़ा अजीबो-ग़रीब है। वे समझते हैं कि इस सृष्टि की व्यवस्था चलानेवाला देवताओं का एक गिरोह है जो अपनी दिलचस्पी की ख़ातिर, मात्र अपने आनन्द की ख़ातिर, मनोरंजन और amusement की प्राप्ति के लिए तरह-तरह के काम करते रहते हैं, जैसे बच्चे समुद्र के किनारे जाएँ तो रेत के घरौंदे बनाते हैं। रेत के ये घरौंदे बनाने से उनका कोई गम्भीर उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मात्र मनोरंजन अभीष्ट होता है। जब इस मनोरंजन से बच्चों का दिल भर जाता है तो वह इन घरौंदों को तोड़-फोड़कर कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह यह पूरी सृष्टि राम की लीला है, एक खेल है।
उसी तरह का खेल जिस तरह बच्चे समुद्र के किनारे रेत के घरौंदे बना-बनाकर खेलते हैं। उसी तरह जब राम का दिल इस लीला से भर जाएगा तो वह इसको तबाह कर देगा। फिर कोई और घर बनाएगा। हिन्दुओं के देवता भी इन घरोंदों पर बच्चों की तरह लड़ते-रहते हैं। जब वे इसी तरह लड़ते हैं, तो कोई और ज़्यादा ताक़तवर देवता आकर उनके घरौंदे तबाह करके रख देता है। यों जिसका वश चलता है वह पहले देवताओं की बसाई हुई दुनिया तबाह कर देता है और अपनी दुनिया बसाता है। इसी तरह यह सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा।
जब पवित्र क़ुरआन ने मक्का मुकर्रमा में एलान किया कि “हमने धरती और आकाश को खेल-कूद में पैदा नहीं किया,” (क़ुरआन, 21:16) तो मक्का मुकर्रमा, बल्कि पूरे अरब द्वीप में शायद किसी को भी हिन्दुओं के इस अक़ीदे (आस्था) का ज्ञान न था। मेरा ख़याल यह है कि पवित्र क़ुरआन के चमत्कार का एक नमूना यह आयत भी है। इसलिए कि न अरब में कोई यह अक़ीदा रखता था और न मक्का मुकर्रमा में, बल्कि शायद उस दौर की सारी सभ्य दुनिया में कोई व्यक्ति हिन्दुओं के इस अक़ीदे से परिचित नहीं था कि हिन्दू इस सारे संसार को राम की लीला समझते हैं और इस पूरी सृष्टि में रचना के प्रतीकों को मात्र देवताओं और बुतों का निरुद्देश्य और अनर्गल खेल समझते हैं। यह आयत ख़ुद इस बात का प्रमाण है कि पवित्र क़ुरआन को आख़िरकार उन क्षेत्रों में जाना था जिन इलाक़ों के लोगों के ये अक़ीदे थे। इस अक़ीदे के खंडन के बाद पवित्र क़ुरआन एलान करता है “हमने धरती और आकाश को केवल एक सत्य की ख़ातिर पैदा किया।” (कुरआन, 44:39) तौहीद (एकेश्वरवाद) का यह अक़ीदा तमाम अक़ीदों का मूल सिद्धान्त है। इस अक़ीदे पर जब इंसान ईमान ले आता है तो शेष सारे अक़ीदों पर ईमान एक तार्किक परिणाम के तौर पर सामने आता रहता है।
अगर इस सृष्टि का एक रचयिता है जो तत्त्वदर्शी है, जिसने एक तत्त्वदर्शिता के साथ और एक उद्देश्य की ख़ातिर यह सृष्टि पैदा की है तो निश्चय ही इस उद्देश्य के परिणाम भी सामने आने चाहिएँ। निष्परिणाम काम तो कोई आम इंसान भी नहीं करता। अत: सृष्टि के रचयिता जिसकी तत्त्वदर्शिता और बुद्धिमत्ता के स्रोत सारी सृष्टि में हर ओर फूटते हैं वह निष्परिणाम कार्य किस प्रकार कर सकता है? देखने में यह आया है कि वह अभीष्ट परिणाम कभी-कभी दुनिया में नज़र नहीं आता। बहुत-से इंसान पूरी ज़िन्दगी क़ुर्बानियाँ देते रहते हैं और मरते दम तक क़ुर्बानियाँ देते चले जाते हैं, लेकिन उन सारी क़ुर्बानियों का तुरन्त उनके अपने लिए बज़ाहिर कोई परिणाम सामने नहीं आता। बज़ाहिर भौतिक दृष्टि से, कारण जगत् की दृष्टि से, उनका जीवन विफल होता है। तो क्या यह सब कुछ ‘अद्ल’ के ख़िलाफ़ नहीं? अगर इंसानों की नेकियों और क़ुर्बानियों का पूरा प्रतिदान यहाँ नहीं मिलता तो क्या उनका परिणाम बाद में आनेवाला है? अगर इंसान ग़ौर करे तो मालूम हो जाएगा कि एक चरण ऐसा आनेवाला है और आना चाहिए, जहाँ इन तमाम कर्मों का परिणाम सामने आए।
यानी अक़ीदा आख़िरत पर ईमान और तौहीद पर ईमान की अनिवार्य अपेक्षा है और अगर इंसान खुले दिल से तौहीद के अक़ीदे पर ग़ौर करे तो वह आख़िरत पर ईमान तक पहुँच जाता है। यही वजह है कि पवित्र क़ुरआन में दर्जनों आयतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह पर ईमान और आख़िरत के दिन पर ईमान को एक साथ बयान किया गया है। इसी तरह बहुत-सी हदीसों में “जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है” जैसे शब्द कई बार एक साथ आए हैं। गोया इन दोनों अक़ीदों पर ईमान और यक़ीन पैदा हो जाए तो तीसरा महत्त्वपूर्ण अक़ीदा यानी पैग़म्बरी और रिसालत पर ईमान का ज़रूरी और अनिवार्य होना ख़ुद-ब-ख़ुद स्पष्ट होकर सामने आ जाएगा।
अगर इन दोनों अक़ीदों, यानी तौहीद और आख़िरत पर ईमान क़ायम हो जाए तो सवाल पैदा होता है कि वह तरीक़ा क्या है जिसके अनुसार सृष्टि का रचयिता चाहता है कि हम ज़िन्दगी गुज़ारें। वह तरीक़ा अगर इंसान मालूम करना चाहे तो वह तरीक़ा केवल पैग़म्बरी और रिसालत है। अल्लाह तआला की तरफ़ से इसका प्रबन्ध मौजूद है कि इंसान को सुथरी और उद्देश्यपूर्ण ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए जिन मौलिक प्रश्नों का उत्तर दरकार है, उन मौलिक प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। इस विषय पर विस्तृत बात आगे जाकर करूँगा, लेकिन संक्षेप के साथ कहा जा सकता है कि अगर इंसान इस सृष्टि पर ग़ौर करे तो पता चलता है कि इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ इस धरती पर मौजूद है। उसको स्वाभाविक रूप से जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वे सब उसके आसपास मौजूद और उपलब्ध हैं। तो क्या ये सवालात स्वाभाविक नहीं हैं? क्या ये सवालात हर इंसान नहीं करता? क्या इंसान को इन सवालों का जवाब मालूम नहीं होना चाहिए? अगर ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और उनके उत्तर इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इंसान के जीवन का गठन और उसके लिए नियमों के संकलन का सारा दारोमदार इन उत्तरों ही पर है तो ये उत्तर भी इंसान को उपलब्ध होने चाहिएँ। जीवन अगर ख़ुद जीवन की गुत्थियों को सुलझानेवाला न हो तो फिर जीवन की ये गुत्थियाँ कौन सुलझाएगा? पैग़म्बरी और रिसालत की संस्था के रूप में इंसानों के मार्गदर्शन का प्रबन्ध और उसकी एक स्वचलित व्यवस्था मौजूद है ताकि इंसानों के मार्गदर्शन का प्रबन्ध होता रहे।
क़ुरआन के कुछ टीकाकारों ने एक उल्लेख उद्धृत किया है जिसमें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इरशाद फ़रमाया कि “दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है और तुम आख़िरत के लिए पैदा किए गए हो।” इस पहलू से थोड़ा-सा ग़ौर करें तो नज़र आता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह इंसानों के फ़ायदे और प्रयोग के लिए है और इंसानों का जीवन उसपर निर्भर है। उनमें से एक चीज़ भी कम हो जाए तो मानव-जीवन बहुत कठिन और कष्टप्रद हो जाएगा, लेकिन अगर ख़ुद इंसान मौजूद न हो तो उनमें से किसी का जीवन कष्टप्रद नहीं होगा। अगर दूध देनेवाले जानवर ख़त्म हो जाएँ तो इंसान दूध की कमी से परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर इंसान मौजूद न हो तो गाय, बैल, बकरी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शायद वे ज़्यादा ख़ुश और आज़ाद रहें। अगर दरख़्त न हों तो इंसान की ज़िन्दगी मुश्किल हो जाएगी। अगर इंसान न हों तो दरख़्तों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दरख़्त इसी तरह फलते-फूलते रहेंगे। इससे मालूम हुआ कि अपने अस्ल अस्तित्व की दृष्टि से हम इन प्राणियों के मुहताज हैं। ये प्राणी हमारे मुहताज नहीं हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह है कि यह प्राणी इंसानों के लाभ और सेवा के लिए पैदा किए गए हैं, इंसानों को उनके फ़ायदे और सेवा के लिए पैदा नहीं किया गया। अब अगर हर चीज़ यहाँ तक कि मामूली-से-मामूली पौधा और कीड़ा भी, इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किया गया है तो यह बात बुद्धि के ख़िलाफ़ है कि इतने बड़े प्राणी इंसान को बिना किसी लाभ और उद्देश्य के पैदा किया गया हो। इंसान का उद्देश्य क्या है? वही बात यहाँ बताई गईं, “निस्सन्देह तुम्हें आख़िरत के लिए पैदा किया गया है।”
यह और इसी तरह की बहुत-सी बातें पवित्र क़ुरआन और हदीसों में जगह-जगह बयान हुई हैं। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का तर्ज़े-अमल ग़ैर-ज़रूरी सवालात करने का नहीं था। उनका रवैया तर्कशास्त्रियों की तरह अकारण बाल की खाल निकालने का नहीं था। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) का तर्ज़े-अमल यह था कि उन्होंने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ज़बान से जो सुना उसपर उसी पल से कार्यान्वयन शुरू कर दिया। प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) अनावश्यक सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन उनमें भी विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व मौजूद थे। कुछ व्यक्तित्व ऐसे थे जिनकी प्रवृत्ति असाधारण रूप से बौद्धिक थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी प्रवृत्ति आसक्तिपूर्ण थी। आसक्तिपूर्ण प्रवृत्तिवाले सहाबा अपने अन्दाज़ से इस्लाम के निर्देशों पर अमल करते थे। बौद्धिक प्रवृत्तिवाले सहाबा अपने अन्दाज़ से शरीअत के आदेशों पर अमल करते थे। इसके दर्जनों, बल्कि सैंकड़ों उदाहरण हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद हैं। एक सहाबी ने एक आदेश पर अमल किया जिसमें बुद्धि, समझ, अन्तर्दृष्टि और तत्त्वदर्शिता की झलक मालूम होती है। एक-दूसरे सहाबी ने उसी आदेश पर ऐसे ढंग से अमल किया जिसमें समर्पण का एक आसक्तिपूर्ण ढंग सामने आता है। लेकिन कार्यान्वयन को निश्चित बनाने में सब प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) समान थे।
ताबिईन के ज़माने में जब ज्ञान-विज्ञान को संकलित करने का काम शुरू हुआ और वे तमाम निर्देश जो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के द्वारा पहुँचे थे, वे ताबिईन ने संकलित करने शुरू कर दिए। इस तरह विषयों की दृष्टि से मामलों और समस्याओं का संकलन शुरू हुआ। कुछ लोग वे थे जिनकी दिलचस्पी यह थी कि शरीअत के विशुद्ध फ़िक़ही पहलू के बारे में मालूमात और निर्देश को जमा किया जाए। कुछ लोगों की दिलचस्पी यह थी कि क़ुरआन और सुन्नत को समझने के लिए अरबी भाषा और साहित्य की गवाहियों और भाषा सौन्दर्य की बारीकियों के बारे में जानकारी को संकलित किया जाए। अरबी शब्दकोश जिसमें पवित्र क़ुरआन अवतरित हुआ उसकी बारीकियाँ क्या-क्या हैं और क़ुरआन किस दृष्टि से भाषा-शैली के ऊँचे दर्जे पर है? वे मालूमात इकट्ठी की जाएँ।
कुछ और लोगों ने इस्लामी अक़ीदों और धारणाओं के बौद्धिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान दिया और इन मालूमात को संकलित ढंग से बयान करना शुरू किया। ताबिईन और तबा-ताबिईन के दौर में जिन लोगों ने सबसे पहले अक़ीदों से सम्बन्धित इन सवालात को उठाया वे अधिकांश मुहद्दिसीन थे। इमाम हसन बस्री (रह॰), इमाम जाफ़र सादिक़ (रह॰), सुफ़ियान सौरी (रह॰), इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰), इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰), इमाम बुख़ारी (रह॰), इन सब लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध इल्मे-हदीस से था। वे हदीसें जिनमें इस्लाम के अक़ीदे और इस्लाम की मौलिक शिक्षा और बुनियादों को बयान किया गया था, वे इन बुज़ुर्गों के विशेष ध्यान का विषय बनीं। आगे चलकर ख़ुद मुहद्दिसीन के वर्ग में ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने विशेष रूप से अक़ीदों की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया।
इन समस्याओं को जमा करने के नतीजे में कुछ ऐसे सवालात पैदा हुए जिनका जवाब देना उन्होंने ज़रूरी समझा। उनमें सबसे पहली समस्या अल्लाह तआला के अस्तित्व और गुणों की थी। अल्लाह तआला का अस्तित्व प्राचीन है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है। अल्लाह तआला के कुछ गुण और असमा-ए-हुस्ना (अच्छे नाम) पवित्र क़ुरआन में बयान हुए हैं। पवित्र क़ुरआन ने इन अस्मा-ए-हुस्ना के लिए ‘सिफ़ात’ के शब्द का प्रयोग नहीं किया। हदीसों में भी ‘सिफ़ात’ का शब्द प्रयोग नहीं हुआ। ‘सिफ़ात’ का शब्द बाद में उलमाए-कलाम ने प्रयोग किया है। पवित्र क़ुरआन में अस्मा का शब्द आया है। अगर मुतकल्लिमीन ‘सिफ़ात’ की शब्दावली प्रयोग न करते और केवल अस्मा का शब्द प्रयोग करते तो शायद बहुत-सी समस्याएँ पैदा न होतीं।
एक सवाल यह पैदा हुआ कि अल्लाह तआला के अस्तित्व और इसकी ‘सिफ़ात’ (गुणों) के दरमियान सम्बन्ध का प्रकार क्या है? जब से अल्लाह तआला का अस्तित्व है, क्या उस समय से ये सारे गुण उसको प्राप्त हैं और वह अल्लाह तआला इन सब गुणों से अनादिकाल से विभूषित है, या कुछ गुणों से बाद में विभूषित हुआ? इसपर विभिन्न लोगों ने विचार व्यक्त किए। हर एक ने अपनी समझ और अपनी बुद्धि के अनुसार पवित्र क़ुरआन और सम्बन्धित हदीसों की टीका और व्याख्या की और उसकी रौशनी में अपने जवाब को पेश किया। लेकिन आम तौर से लोगों, मुहद्दिसीन और टीकाकारों का कहना यह था कि जब से अल्लाह तआला का अस्तित्व है उसी समय से वह अलीम (सर्वज्ञ) भी है और क़दीम (प्राचीन) भी, उसी समय से वह ख़ालिक़ (रचयिता) भी है और समीअ और बसीर (सबकी सुननेवाला और सब कुछ देखनेवाला) भी और ये सारे गुण उसे शुरू से ही प्राप्त हैं।
कुछ अन्य लोगों का कहना यह था कि उनमें से कुछ गुण अल्लाह तआला ने बाद में अपनाए हैं। और आवश्यकतानुसार उसने पैदा किए हैं। इन बाद के लोगों का ख़याल था कि अल्लाह तआला अपने नए-नए गुणों को पैदा करता रहता है, इन गुणों को पैदा करने के नतीजे में इन गुणों की निशानियाँ भी सामने आती हैं। यह एक विशुद्ध दार्शनिकतापूर्ण या बौद्धिक मामला था। इन दोनों दृष्टिकोणों के समर्थकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के समर्थन में तर्क देने शुरू किए। इस तरह एक ऐसी कला अस्तित्व में आई जिसको आगे चलकर इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) कहा गया (इसपर आइन्दा चर्चा होगी)।
इन हालात में इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इससे पहले कि यह विशुद्ध बौद्धिक और अव्यावहारिक तर्कशास्त्रीय प्रश्न जनसाधारण के ज़ेहन को किसी उलझन में मुब्तला करें, इस्लाम के अक़ीदों को इस तरह स्पष्ट ढंग से बयान कर दिया जाए कि आम आदमी किसी शक-सन्देह में मुब्तला न हो। हर वह हिदायत और हर वह चीज़ जिसकी रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने शिक्षा दी, जो पवित्र क़ुरआन में स्पष्ट रूप से बयान हुई है या सुन्नत में स्पष्ट रूप से आई है, उसपर ईमान लाना ज़रूरी है। एक पहलू से वह इस्लाम के अक़ीदे का हिस्सा है।
पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-रसूले के भंडार में जो कुछ आया है उसके मूल रूप से दो प्रकार हैं। एक के बारे में पूर्ण तार्किक शब्दावली प्रयुक्त होती है जबकि दूसरी प्रकार के बारे में अनुमानित शब्दावली प्रयुक्त होती है। यानी एक आदेश वह है जो अपने मानी और मतलब के निर्धारण में बिलकुल निश्चितता के साथ स्पष्ट है, उसके मानी और मतलब में एक से अधिक व्याख्याओं की गुंजाइश नहीं है। कुछ आयतें और हदीसें ऐसी भी हैं जहाँ एक से अधिक व्याख्याओं की गुंजाइश मौजूद है। वहाँ एक से अधिक व्याख्याओं की गुंजाइश इसलिए है कि अल्लाह तआला की नियति ने वहाँ ऐसा कोई वर्णन शैली या शब्द प्रयोग किया है जिसकी एक से अधिक व्याख्याएँ सम्भव हैं। अगर पवित्र क़ुरआन में कोई ऐसा शब्द आया है जिसके अरबी भाषा, शब्दकोश और नियमों के अनुसार एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं तो उसके मानी केवल यह हैं कि अल्लाह तआला ने यह चाहा कि लोग उसकी एक से अधिक व्याख्याएँ करें या करने में आज़ाद हों। जहाँ मामला किसी निश्चित रूप से तार्किक शिक्षा का था वह इसलिए था कि अल्लाह तआला ने चाहा कि इस आदेश या निर्देश का एक ही अर्थ समझा जाए। अब जहाँ तक पूर्ण तार्किकता के मामलात हैं उनमें तो कोई ज़्यादा मतभेद पैदा नहीं हुआ। जो आयतें अनुमानित तर्कों पर आधारित हैं उनके बारे में एक से अधिक व्याख्याएँ और टीकाएँ सम्भव हैं और शब्दकोश और शरीअत के नियमों की सीमाओं में एक से अधिक व्याख्याएँ हर दौर में सम्भव रहेंगी। एक तक़सीम तो यह है जिसपर में अभी आता हूँ।
दूसरी तक़सीम थी पक्के प्रमाण और अनुमानित प्रमाण की। यानी शरीअत की शिक्षा का एक हिस्सा तो वह है जिसका अल्लाह द्वारा अवतरित वह्य (प्रकाशना) होना निश्चित रूप से मालूम है और साबित है, जैसे पवित्र क़ुरआन और सुन्नते-मुतवातिरा या सुन्नते-साबिता। इसके बारे में कोई शक-सन्देह नहीं कि यह रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षा है, वह क़ुरआन के रूप में हो या सुन्नत के रूप में। लेकिन सुन्नत का एक हिस्सा वह भी है जो ‘ज़न्नियुस-सुबूत’ (अनुमानित) कहलाता है यानी किसी एक रावी (उल्लेखकर्ता) या दो रावियों की रिवायत के आधार पर क़ायम है, किसी एक सहाबी की रिवायत पर क़ायम है या किसी एक ताबिई की रिवायत पर क़ायम है जिसके बारे में टीकाकारों और मुहद्दिसीन का मतैक्य है कि यह ‘ज़न्नियुस-सुबूत’ है। अब यह बात कि पवित्र क़ुरआन या शरीअत के अनुसार जो चीज़ अक़ीदे की हैसियत रखती है जिसपर मुसलमानों का ईमान लाना ज़रूरी है वह क्या है? इसपर इस्लामी विद्वानों का मतैक्य है कि अक़ीदे का अस्ल दारोमदार किसी ऐसे आदेश या ‘नस्स’ पर नहीं हो सकता जो ‘ज़न्नियुस-सुबूत’ और ज़न्नियुद-दलाला (अनुमानित तर्कों पर) हो। अक़ीदे का सुबूत पूर्ण तार्किक और पूर्णतः प्रमाणित आदेशों ही के आधार पर होगा। ‘ज़न्नियुस-सुबूत’ और अनुमानित तर्कों के आधार पर किसी एक व्याख्या से अक़ीदा साबित नहीं होता। उदाहरणार्थ ज़न्नियुद-दलाला का एक बड़ा प्रकार मुतशाबिहात (उपलक्षित आयतें) हैं। पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है कि इस किताब की कुछ आयतें हैं जो मुहकमात हैं, कुछ आयतें हैं जो मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात के शाब्दिक अर्थ हैं वे चीज़ें जो मिलती-जुलती हों। जो एक-दूसरे से समानता रखती हों। लेकिन टीकाकारों का कहना है कि मुतशाबिहात की इस ख़ास शब्दावली से मुराद वह शैली या वर्णन शैली है जो पराभौतिक और परोक्ष तथ्यों को बयान करने के लिए पवित्र क़ुरआन में प्रयुक्त हुई है। पवित्र क़ुरआन में इंसानों की समझ से क़रीब करने की ख़ातिर अल्लाह तआला ने अपने बारे में, आख़िरत की ज़िन्दगी के बारे में, अपनी क़ुदरत और अपनी सत्ता की विशालता के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बयान किए हैं जिनकी वास्तविकता का आभास मानव-बुद्धि की क्षमता और सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए ये तथ्य इंसान की समझ की ख़ातिर, इंसानों की भाषा और इंसानों की शैली में बयान किए गए हैं।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ‘हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा’ में एक जगह लिखा है कि अल्लाह तआला की महानता और उसकी बड़ाई और शान के प्रताप का वास्तविक अनुमान और आभास इंसान कभी नहीं कर सकता, इंसान को अन्दाज़ा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तआला की महानता, बुज़ुर्गी और पाकीज़गी किस शान और किस बुलन्द मर्तबे की है। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह तआला की महानता और शान की कुछ-न-कुछ कल्पना इंसानों के ज़ेहन में बिठाने के लिए इंसानों के अवलोकन के अनुसार वर्णन शैली पवित्र क़ुरआन में अपनाई गई है। इंसानों के अनुभव में जो बड़ी-बड़ी चीज़ें आती हैं वे अल्लाह तआला की बड़ाई को समझाने के लिए प्रयोग की गई हैं। इंसान बादशाहों को और बड़े-बड़े शासकों को देखता है जिनके प्रभाव से बड़े-बड़े लोग डरते रहते हैं। बादशाहों के पास फ़ौजें होती हैं, उनके लश्कर होते हैं, उनके पास तख़्ते-शाह होते हैं, सज़ा देनेवाले जल्लाद और आदेश का अनुपालन करनेवाले कारिंदे होते हैं। इन सब कारणों और संसाधनों को देखकर बादशाह या शासक की महानता का एहसास एक इंसान के दिल में क़ायम हो जाता है। अल्लाह तआला की महानता और बुजु़र्गी को बयान करने के लिए पवित्र क़ुरआन और हदीसों में यही शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं और उन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है जो बादशाहों के लिए प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ अल्लाह तआला की फ़ौजें, लश्कर, तख़्त आदि। हालाँकि दर-हक़ीक़त अल्लाह तआला को उनमें किसी की ज़रूरत नहीं, न फ़ौज की ज़रूरत है न तख़्त की। ये तो इंसानों की आवश्यकताएँ हैं। लेकिन इंसानों की समझ चूँकि इन कारणों और संसाधनों से अवगत है इसलिए अल्लाह तआला की महानता और बड़ाई के विषय को इंसानों की समझ से क़रीब लाने के लिए ये इंसानी शब्द अल्लाह तआला और उसके पैग़म्बर ने प्रयोग किए हैं।
एक जगह आया है कि “तुमने ख़ाक फेंकी, तो तुमने न फ़ेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी।” (क़ुरआन, 8:17) या “अल्लाह तआला का हाथ उनके हाथ के ऊपर था।” (क़ुरआन, 48:10) एक और जगह यह भी आया है कि “कोई चीज़ अल्लाह जैसी नहीं हो सकती।” (क़ुरआन, 42:11) जब अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती तो मेरा हाथ अल्लाह के हाथ जैसा कैसे हो सकता है? और अल्लाह का हाथ मेरे हाथ जैसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो ‘‘यदुल्लाह’’ से क्या मुराद है? क्या ‘यदुल्लाह’ से सांकेतिक अर्थ में अल्लाह तआला की शक्ति और दस्ते-क़ुदरत मुराद है? या अल्लाह तआला का कोई हाथ है जिसकी अपना कोई ख़ास प्रकार है। जिसको हम नहीं जानते? या इसी तरह का हाथ है जिसको हम हाथ कहते हैं? यहाँ ‘यदुल्लाह’ की व्याख्या में यही तीन स्थितियाँ सम्भव हैं। यही तीन व्याख्याएँ हो सकती हैं। या तो यह कहा जाए कि ‘यदुल्लाह’ से मुराद एक ऐसा हाथ है जिसकी पाँच उंगलियाँ हों और वह बहुत बड़ा हाथ हो, यह एक अर्थ है और कुछ सतह-बीं और ज़ाहिर-परस्तों का यही दृष्टिकोण रहा। अस्हाबे-ज़वाहिर यही कहते थे। कुछ और लोगों का कहना था कि अल्लाह तआला को ‘यद’ प्राप्त है, लेकिन उसका प्रकार क्या है? उसकी कैफ़ियत क्या है? वह हम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह तआला का एक हाथ है जिसके लिए ‘यद’ का अरबी शब्द पवित्र क़ुरआन में प्रयोग हुआ है। इसके प्रकार और वास्तविकता को अल्लाह तआला ही जानता है। यह दृष्टिकोण इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) और अशाइरा का है। तीसरा दृष्टिकोण अधिकांश हनफ़ी उलमा और मातुरीदिया का है, वे कहते हैं कि इससे मुराद अल्लाह तआला का दस्ते-क़ुदरत है। अल्लाह तआला का अधिकार और शासन है, जिससे अल्लाह तआला इंसानों को सौभाग्य प्रदान करता है। इंसानों को उससे लाभान्वित करता है।
ये और इस प्रकार की आयतें हैं जो मुतशाबिहात कहलाती हैं। अब मुतशाबिहात के इन तीन सम्भावित अर्थों में किस अर्थ को अपनाया जाए, किस अर्थ को न अपनाया जाए? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि इन सम्भावित अर्थों में से कोई निर्धारित अर्थ और कोई एक दृष्टिकोण अपनाना इस्लामी अक़ीदे की अनिवार्य अपेक्षा नहीं। इन सब में से कोई एक अर्थ दीन की आवश्यकताओं की हैसियत नहीं रखता, इस मानी में कि एक निर्धारित अर्थ स्वीकार करना मुसलमान होने की अनिवार्य शर्त हो, ऐसा नहीं। उनमें से जिस धारणा के अनुसार भी एक माननेवाला ‘यदुल्लाह’ की धारणा रखता है वह मुसलमान है। और उसके बारे में समझा जाएगा कि वह पवित्र क़ुरआन और उसकी तमाम आयतों पर ईमान रखता है। अलबत्ता विद्वान अगर तर्कों से किसी एक अर्थ को स्वीकार्य और दूसरे को अस्वीकार्य और कमज़ोर क़रार दें तो इसकी गुंजाइश हमेशा मौजूद रही है। यह और इस तरह के प्रश्न ताबिईन के ज़माने में सामने आने शुरू हुए। जब इस तरह का कोई सवाल पैदा होगा, तो ज़ाहिर है उसके सन्दर्भ में ऐसे पेचीदा सवालात और नाज़ुक मामलात भी चर्चा में आएँगे कि जिनसे आम आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसके अलावा इंसानों की विशेषता है कि जब कोई वैचारिक बहस शुरू होती है तो ऐसी-ऐसी बातें इंसान के ज़ेहन में आती हैं जिसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं होती। लेकिन बौद्धिक प्रश्नों से दिलचस्पी रखनेवाले उनसे बहस करते रहते हैं। इन समस्याओं की व्यावहारिक उपयोगिता न होने की वजह से अक्सर सावधानी प्रिय बुज़ुर्गों, सहाबा और ताबिईन ने इस तरह की बहसों को पसन्द नहीं किया। जो लोग इन बहसों में अपना समय लगाते थे उनकी इस सरगर्मी को अक्सर विद्वानों ने कोई लाभकारी और स्वीकार्य गतिविधि नहीं समझा।
लेकिन यह सीमाबन्दी कहाँ की जाए कि यहाँ तक तो यह गतिविधि लाभदायक और ज़रूरी है और इस हद के बाद अब अनावश्यक और अलाभकारी क़रार दी जानी चाहिए। यह सीमाबन्दी इसलिए मुश्किल है कि इंसानी ज़ेहन में सवाल तो पैदा होंगे। सवाल पैदा होंगे तो उनका जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन उन सवालों के पैदा होने की सूरत में किस तरह इस बात का प्रबन्ध किया जाए कि जहाँ तक व्यावहारिक ज़रूरत है, वहाँ तक सवाल पैदा हों, उससे आगे सवाल पैदा न हों। इसके बारे में हदीसों में भी निर्देश मौजूद हैं। एक प्रसिद्ध हदीस सहीह मुस्लिम में आई है। अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि तुम्हारे ज़ेहन में तरह-तरह के सवालात पैदा होंगे, फिर एक सवाल शैतान तुम्हारे ज़ेहन में डालेगा कि जब हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो ख़ुदा को किसने पैदा किया? तो जब इस तरह के सवालात अल्लाह के वुजूद के बारे में आएँ तो तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की पनाह माँगो और इस तरह के सवालात उठाने से रुक जाओ।
इससे यह पता चला कि बौद्धिक प्रश्न और वैचारिक वाद-प्रतिवाद में एक चरण प्रश्नों का ऐसा आता है और आ सकता है जो इंसान की बुद्धि से बाहर हो। इंसान के बस से बाहर हो। अब बजाय इसके कि इंसान एक ऐसे इलाक़े में क़दम रखे जिसमें क़दम रखने के वह योग्य नहीं है और जिसकी वह दरकार क्षमता नहीं रखता, जहाँ उसको असफलता का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर यह है कि पहले दिन ही से वह यह एहसास रखे कि उसकी सीमाएँ क्या हैं और उनको किन मामलात में जाना चाहिए, किन मामलात में नहीं जाना चाहिए।
इस तरह के विशुद्ध बौद्धिक प्रश्नों के मामले में विद्वानों की दो तरह की दिलचस्पियाँ सामने आईं। एक दिलचस्पी तो यह थी कि आम आदमी को जो इन बहसों से अवगत नहीं है उसको इन वैचारिक बहसों से कैसे मुक्त किया जाए (ज़ाहिर है इन बहसों से दिलचस्पी रखनेवाले एक प्रति हज़ार भी नहीं होते, एक प्रति लाख भी मुश्किल से होते होंगे। इसलिए कि बौद्धिकतावादी लोग बहुत थोड़े लोग होते हैं, कुछ सौ से ज़्यादा नहीं होते)। अब इन कुछ सौ व्यक्ति के सवालों का बोझ लाखों, करोड़ों इंसानों पर अकारण क्यों डाल दिया जाए और लाखों-करोड़ों इंसानों को ग़ैर-ज़रूरी उलझन और परेशानी का शिकार क्यों कर दिया जाए, यह कोई तत्त्वदर्शिता और समझदारी का तरीक़ा नहीं।
इसलिए इस्लामी विद्वानों ने पहला काम तो यह किया कि उन्होंने ईमान का एक फ़ार्मूला संकलित किया जो कुछ हदीसों पर आधारित और पवित्र क़ुरआन की आयतों से लिया गया है। जिसको आम शब्दावली में ‘ईमाने-मुजमल’ के नाम से याद करते हैं। ‘ईमाने-मुजमल’ यानी उन मौलिक तथ्यों की पुष्टि और इक़रार जिनका ज़िक्र पवित्र क़ुरआन या मुतवातिर और प्रमाणित हदीसों में है। ‘ईमाने-मुजमल’ के इस फ़ार्मूले का उद्देश्य यह था कि जिन तथ्यों को अक़ीदे में आधार का दर्जा प्राप्त है वे इंसानों के ज़ेहनों में बैठ जाएँ और यह बात उनके ज़ेहन में हर वक़्त ताज़ा रहे कि इंसानों के अक़ीदे ये होने चाहिएँ। अल्लाह तआला पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान और आख़िरत के इनाम और सज़ा तथा तक़दीर यानी भाग्य पर ईमान। यह ‘ईमाने-मुजमल’ है। फिर इन अक़ीदों का और अधिक विवरण ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ कहलाता है। ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ के विभिन्न दर्जे हैं। मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने हर दौर में नए-नए अन्दाज़ से उन विवरणों को बयान किया है, और अक़ीदे की बहसों की विभिन्न वैचारिक और ज्ञानपरक स्तरों पर व्याख्या की है। जिस स्तर का इंसान होगा उसको उसी स्तर के ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ की बहसों को जब भी ज्ञानपरक ढंग से बयान किया जाएगा तो सम्बन्धित ज़माने और इलाक़े की मानसिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को सामने रखना अनिवार्य होगा।
उदाहरण के रूप में अगर आप इस्लाम का कोई अक़ीदा आज पाकिस्तान के सन्दर्भ में पाकिस्तान के आधुनिक और उच्च शिक्षा प्राप्त या आम शिक्षा प्राप्त श्रोताओं के क्षेत्र में बयान करेंगे तो आपकी शैली और अन्दाज़ अल्लामा तफ़्ताज़ानी और सैयद शरीफ़ जुर्जानी की शैली और अन्दाज़ से निश्चय ही भिन्न होगा। अल्लामा तफ़्ताज़ानी और सय्यद शरीफ़ जुर्जानी की तर्क शैली और उनके अन्दाज़ की बहस मस्जिद में ख़तीब लोग या यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर लोग बयान करेंगे तो हर कोई नहीं समझेगा, बल्कि बहुत-से लोग और अधिक उलझन का शिकार होंगे। इसलिए कि तफ़्ताज़ानी और सय्यद शरीफ़ जुर्जानी ने अपने-अपने ज़माने में अपनी वैचारिक समस्याओं और मामलों को सामने रखते हुए एक ख़ास तर्क शैली में इस्लाम के अक़ीदों को पेश किया था। आज इस तर्क शैली और वर्णन शैली से अधिकांश लोग अपरिचित हैं। इतनी बात तो स्पष्ट है कि इस्लामी अक़ीदों की व्याख्या और स्पष्टीकरण में जो शैली इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) की थी वह इमाम ग़ज़ाली की नहीं थी। जो वर्णन शैली इमाम ग़ज़ाली ने अपनाई थी वह तफ़्ताज़ानी की नहीं थी। तर्क देने का जो तरीक़ा तफ़्ताज़ानी का था वह सैयद अहमद शहीद का नहीं था, जो समझानेवाली शैली शैख़ अहमद सरहिन्दी की थी वह अल्लामा इक़बाल की नहीं थी।
इससे पता चला कि अक़ीदे की फ़ार्मुलेशन या ‘ईमाने-मुफ़स्सल’ की articulation हर ज़माने के वैचारिक स्तर और ज्ञानपरक, वैचारिक तथा सांस्कृतिक मापदंड के अनुसार होगी। फ़ार्मुलेशन में अन्तर का अर्थ यह नहीं है कि ईमान की वास्तविकता में अन्तर है या ‘ईमाने-मुजमल’ जो हमेशा इसी तरह रहेगा उसके विवरण में कोई अन्तर है। विवरणों में अन्तर नहीं होगा। ईमानियात की बुनियादें वही रहेंगी, अक़ीदों के आधारभूत नियम वही रहेंगे। अलबत्ता उनके बयान, उनकी शैली और उनको पेश करने के अन्दाज़ में अन्तर होगा।
एक बड़ी मौलिक चीज़ तो अक़ीदों के बारे में यह ज़ेहन में रहनी चाहिए। दूसरी बड़ी मौलिक बात यह है कि कभी-कभी अक़ीदों की बहसों में कुछ ऐसे सवालात भी आ जाते हैं जिनका सम्बन्ध अक़ीदे से नहीं, बल्कि अमल से होता है। अगरचे इन सवालों का अस्ल सम्बन्ध अमल से होता है, लेकिन किसी वजह से वे अक़ीदे की बहस का हिस्सा भी बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में एक छोटी-सी किताब है, किताब ‘अल-फ़िक़्हुल-अकबर’ जो हज़रत इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की बताई जाती है। यह पुस्तक या पुस्तिका या तो इमाम साहब की अपनी लिखी हुई है, या इमाम साहब के तुरन्त बाद उनके किसी शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्दं की लिखी हुई है। लेकिन यह बात सब मानते हैं कि यह किताब अक़ीदों पर प्राचीनतम लेखों में से एक है। किताब ‘अल-फ़िक़्हुल-अकबर’ में लेखक ने उन मौलिक अक़ीदों की निशानदेही की है जो ‘अहले-सुन्नत वल-जमाअत’ को दूसरों से अलग करते थे। याद रहे कि मुसलमानों में जो फ़िरक़े या वर्ग पैदा हुए वे अक़ीदों ही में इख़तिलाफ़ के आधार पर पैदा हुए। इन फ़िर्क़ों में शीया, ख़ारिजी और मोतज़िली पहली शताब्दी के अन्त और दूसरी हिजरी के आरम्भ से नुमायाँ हुए। उनसे मुसलमानों के अधिकांश उलमा का मतभेद अक़ीदों ही के मामले में था। उनके ख़यालात के मुक़ाबले में अहले-सुन्नत के अक़ीदों को बयान करने की ज़रूरत इमाम साहब ने या उनके शागिर्दों में से किसी ने महसूस की और यह पुस्तिका संकलित की। इन फ़िर्क़ों में से शीया फ़िर्क़े के लोग ‘मस्हे-ख़ुफ़्फ़ैन’ (चमड़े की जुराबों पर मस्ह) को या ‘मस्हे-जौरबैन’ (सूत की जुराबों पर मस्ह) को दुरुस्त नहीं समझते थे। जौरबैन पर या ख़ुफ़्फ़ैन पर मस्ह (वुज़ू के वक़्त किसी अंग पर गीला हाथ फेरना) जायज़ है या नाजायज़ है, यह एक विशुद्ध फ़िक़ही और व्यावहारिक मामला है। इसका अक़ीदे से कोई सम्बन्ध नहीं। जैसा कि वुज़ू का, तयम्मुम का या अन्य फ़िक़ही मामलों का अक़ीदे से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह विशुद्ध फ़िक़ही समस्याएँ हैं, लेकिन अगर कोई फ़िक़ही मसला ऐसा हो कि वह निश्चित तर्कों और निश्चित सुबूतों से साबित हो और उसका कोई गिरोह इनकार करे तो फिर वह मसला अक़ीदे की सीमाओं में दाख़िल हो जाता है। इसलिए कि जब किसी क़ानून के क़ानून होने का इनकार किया जाए तो बात क़ानून के सिद्धान्त से परे दायरे में दाख़िल हो जाती है। इस तरह किसी स्पष्ट फ़िक़ही आदेश के न मानने से अक़ीदे की बात आ जाती है और यह अक़ीदे का मसला बन जाता है। इसलिए कि आप आग्रह करेंगे कि यह आदेश निश्चित तर्कों पर है और पक्का सुबूत है और साहबे-शरीअत से साबित और निश्चित और यक़ीनी तौर पर लिया गया है। अगर वह इससे इनकार करता है कि यह आदेश साहबे-शरीअत से उद्धृत नहीं है तो साहबे-शरीअत से उद्धृत होना या न होना मात्र फ़िक़ही मसला नहीं रहता, अब यह अक़ीदे का मसला बन जाता है। इसलिए इस तरह के कुछ व्यावहारिक मामले कुछ हालात में अक़ीदे का मसला बन गए जो दरअसल अक़ीदे का मसला नहीं थे।
इससे अन्दाज़ा होगा कि अक़ीदे की बहसों में विभिन्न ज़मानों में कुछ नई समस्याओं की वृद्धि होती रही है। इन समस्याओं की वृद्धि इसलिए हुई कि कोई ऐसा दृष्टिकोण सामने आ गया जो इस्लामी शिक्षाओं से मेल नहीं खाता, बल्कि उनसे टकराता था और इस दृष्टिकोण को मानने के नतीजे में किसी ऐसे प्रमाणित आदेशों का इनकार हो रहा था जो साहबे-शरीअत (अल्लाह के रसूल) से उल्लिखित हैं और निश्चितता के साथ उल्लिखत हैं। इसलिए उसकी हैसियत अक़ीदे की बन गई। जब उसकी हैसियत अक़ीदे की बन गई तो इस्लामी विद्वानों ने उसको अक़ीदों की किताब में शामिल कर लिया।
अक़ीदों के बारे में बहस यों तो क़ुरआन के टीकाकारों ने भी की है और हर बड़े टीकाकार ने पवित्र क़ुरआन की उन आयतों की व्याख्या भी की है जो अक़ीदों से बहस करती हैं। हर मुहद्दिस ने उन हदीसों पर भी बहस की है जो अक़ीदों से सम्बन्धित हैं। इसी तरह से कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने उन मामलात से भी बहस की है जो बाद में चलकर अक़ीदे का हिस्सा बन गए। इसी तरह कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को लोगों के मतभेद की शिद्दत ने अक़ीदे का हिस्सा बना दिया। हालाँकि वह ऐतिहासिक घटना थी जिसके घटित होने या न होने के बारे में इतिहास के शोधकर्ताओं में मतभेद हो सकता है। कोई विशेष घटना इतिहास में घटित हुई या नहीं हुई इसमें एक से अधिक मत हो सकते हैं। लेकिन किसी गिरोह के यहाँ अपनी राय या शोध के बारे में शिद्दत पैदा हो गई और उसने एक ख़ास दृष्टिकोण से किसी घटना के होने या न होने पर आग्रह किया और यों वह अक़ीदे का हिस्सा बन गया। होते-होते इस तरह की कुछ फ़िक़ही बहसें और ऐतिहासिक घटनाएँ और मामलात भी अक़ीदों में शामिल हो गए।
ईमान के परिपक्व होने और उसके स्थायित्व के लिए अक़ीदे की ज़रूरत का एक पहलू और भी है। जिस तरह इस सृष्टि में ख़ला (शून्य) का भौतिक रूप में होना सम्भव नहीं है इसी तरह से अक़ायदी और नज़रियाती रिक्तता भी सम्भव नहीं है। अगर अक़ायदी रिक्तता होगी तो कोई दूसरा अक़ीदा आकर उस रिक्त स्थान को भर देगा। आज की फ़िज़िक्स यही बताती है कि जब कोई ख़ला या रिक्त स्थान पैदा होगा तो कोई चीज़ आकर उस रिक्त स्थान को भर देगी और वह रिक्त स्थान या शून्य बाक़ी नहीं रहेगा। यही मामला अक़ीदे का है कि कोई अक़ायदी या दावती रिक्त स्थान इंसानी समाज में ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता। जल्द ही कोई-न-कोई अक़ीदा, ग़लत या सही, इस ख़ाली जगह को पुर कर देता है। अत: शरीअत की कोशिश यह है कि अक़ीदे की दृष्टि से कोई रिक्तता इंसानों के ज़ेहनों में मौजूद न रहे। इसलिए कि अगर ख़ालीपन मौजूद होगा तो कोई दूसरी दावत या कोई दूसरा अक़ीदा उसको भर देगा। फिर अगर इंसान सामूहिक जीव और नागरिक पशु है तो फिर उसको चिन्तक जीव भी होना चाहिए। कुछ मुसलमान चिन्तकों ने यह लिखा है कि इंसान मात्र सामूहिक पशु या सभ्य जानवर नहीं है, बल्कि चिन्तक जीव भी है। एक पश्चिमी विद्वान, सम्भवतः रेने देकार्त (René Descartes) ने लिखा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी उसके अस्तित्व का सबसे मज़बूत और वास्तविक प्रमाण उसका चिन्तक होना है। अपने अस्तित्व की दलील वह यह देता है कि मैं सोचता हूँ और चूँकि मैं सोचता हूँ अत: मेरा अस्तित्व वास्तविक है।
अगर इंसान चिन्तक पशु भी है तो वह अवश्य ही इंसान धार्मिक पशु भी है। मानव इतिहास के तमाम सुबूतों से पता चलता है कि जब से इस सृष्टि में इंसान है वह धार्मिक भी रहा है। उसपर अल-जज़ाइर के बड़े चिन्तक मालिक-बिन-नबी ने अपनी किताब ‘अज़-ज़ाहिरुल-क़ुरआनियः’ में बड़ी विद्वतापूर्ण चर्चा की है। उन्होंने प्राचीन अवशेषों, इतिहास और मनुष्य जाति के विज्ञान यानी anthropology से यह साबित किया है कि जब से दुनिया में इंसान है उसी समय से धर्म का अस्तित्व भी साबित है। आधुनिक काल की आध्यात्मिक दृष्टि से अभागे इंसान के अलावा अतीत के किसी दौर में भी ऐसे किसी मानव समाज का अस्तित्व नहीं मिलता जो पूर्ण रूप से सृष्टि के रचयिता के इनकार का अक़ीदा रखता हो। इसलिए कि रचयिता पर ईमान इंसानियत की एक स्वाभाविक अपेक्षा है, जिसकी तरफ़ पवित्र क़ुरआन में कई बार इशारा किया गया, “यह अल्लाह की पैदा की हुई प्रकृति है जिसपर उसने लोगों के पैदा किया है।” (क़ुरआन, 30:30) इंसान स्वाभाविक रूप से धर्म प्रिय और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ रखनेवाला है और नास्तिकता न केवल आज एक अपवाद की हैसियत रखती है बल्कि अतीत में भी विशुद्ध नास्तिकता और दहरियत एक अपवाद की हैसियत रखती थीं। अधर्मी लोग आज भी अल्पसंख्या में हैं और उनको बाहुल्य कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। यही वह चीज़ है जिसको पवित्र क़ुरआन की विभिन्न आयतों और हदीसों में विभिन्न अन्दाज़ में बयान किया गया है।
जहाँ तक ‘अह्दे-अलस्त’ की बात है तो इसकी व्याख्या में विभिन्न टीकाकारों ने अपने-अपने ढंग से विभिन्न व्याख्याएँ की हैं। कुछ विद्वानों ने इसको सांकेति और अलंकार के रंग में देखा है, कुछ ने इसे वास्तविकता का रंग दिया है, कुछ अन्य टीकाकारों ने इसे एक और अलग अन्दाज़ से देखा है। लेकिन इस बात पर सब सहमत हैं कि इस आयत का मूल आशय यह बताना है कि सृष्टि के रचयिता पर ईमान इंसान की प्रकृति में शामिल है। अपने नैसर्गिक प्रेरक ही के कारण इंसान सृष्टि के रचयिता के सामने पेश होना चाहता है, उसके सामने विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहता है। यह वही बात है जिसको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने प्रसिद्ध हदीस कि “हर पैदा होनेवाला बच्चा स्वाभाविक प्रकृति पर पैदा होता है” और यह स्वाभाविक प्रकृति उसके अस्तित्व में उस समय तक क़ायम रहती है जब तक उसके माँ-बाप या माहौल या समाज उसको उससे घृणा न दिला दे। प्रकृति से घृणा करनेवाली चीज़ें कृत्रिम, ज़ाहिरी और अस्थायी हैं, जबकि स्वाभाविक प्रकृति वास्तविक है। प्रकृति अल्लाह के अस्तित्व और उसपर ईमान पर आधारित है।
जब इस्लामी चिन्तकों और क़ुरआन के टीकाकारों ने अक़ीदों और ईमानियात पर चर्चा का आरम्भ किया तो एक महत्त्वपूर्ण सवाल यह पैदा हुआ कि इंसानों के ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान के स्रोत का सवाल तमाम ज्ञान-विज्ञान में मौलिक हैसियत रखता है। यह सम्भवतः एक ऐसा विषय है जो इंसान के हर मानसिक प्रयास, हर सांस्कृतिक प्रयास और हर सामाजिक प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाता है। इंसान ज्ञान कैसे और कहाँ से प्राप्त करता है? पश्चिमवालों ने केवल इस ज्ञान या उस वास्तविकता का अस्तित्व स्वीकार किया है जो देखने से सामने आ रही हो या अवलोकन उसे वास्तविकता मानता और इसको महसूस करता हो, शेष चीज़ों के अस्तित्व से या तो पश्चिमवालों ने इनकार किया है या उसके बारे में शक का इज़हार किया है। अत: ऐसे बहुत-से तथ्य जो मुसलमान की नज़र में अकाट्य तथ्यों की हैसियत रखते हैं वे पश्चिमी शिक्षित व्यक्ति की नज़र में विचारणीय हैं या उनका अस्तित्व सन्दिग्ध है या फिर वे अवास्तविक और सांकेतिक प्रकार के हैं।
ये बात पश्चिमवालों में इस वजह से पैदा हुई कि जब उनके यहाँ वैज्ञानिक विकास ने एक विशेष आयाम ले लिया और वैज्ञानिक विकास और खोजों ने बहुत-से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया तो हर चीज़ पर विज्ञान के दृष्टिकोण से ग़ौर करने की प्रवृत्ति पैदा हो चली। विज्ञान का मैदान चूँकि अनुभवों एवं अवलोकनों का मैदान है इसलिए ज़ाहिरी अनुभव और महसूस होनेवाला अवलोकन ही हर बात के सत्यपरक होने का अस्ल मानदंड समझा जाने लगा। यहाँ तक कि नैतिकता और आध्यात्मिकता के मामले में भी अनुभव और अवलोकन के वास्तविक मानदंड होने की बात की जाने लगी।
यह शैली जिसको बेकन ने वैज्ञानिक विधि के नाम से याद किया, आंशिक बातों और व्यक्ति के आंशिक अवलोकनों से एक सिद्धान्त निकालता है। यह वस्तुतः ‘इस्तिक़रा’ (निश्चितता) का सिद्धान्त है जो मुसलमान चिन्तकों ने खोजा था। पवित्र क़ुरआन ने सबसे पहले ‘इस्तिक़रा’ का सिद्धान्त दिया था। इससे पहले दुनिया ‘मंतिक़े-इस्तिख़राजी’ (अनुमानित तार्किकता) से परिचित थी जो अल्पसंख्यकों और एकाकी विचारों की दुनिया में तो सफल बताई जाती है, अगरचे वहाँ भी सफल थी कि नहीं थी इसके बारे में दोराएँ हो सकती हैं लेकिन अनुभवों एवं अवलोकनों के मैदान में इसका चरित्र और उपयोगिता न होने के बराबर है। ‘मंतिक़े-इस्तिक़राई’ से दुनिया वास्तविक रूप से पवित्र क़ुरआन के अवतरण के बाद ही से परिचित हुई। मुसलमान चिन्तकों में इब्ने-मस्कवैह, ग़ज़ाली, इब्ने-सीना और फ़ाराबी ने मंतिक़े-इस्तिक़राई के सिद्धान्तों को ज़्यादा संकलित ढंग से पेश किया। यहीं से यह चीज़ बेकन और दूसरे पश्चिमी चिन्तकों तक पहुँची।
जब उन्होंने देखा कि जिस चीज़ की वे दिन-रात परवाह करते हैं, जिन सच्चाइयों और अनुभवों का वे रोज़ अवलोकन करते हैं, उनके आधार पर वे बहुत कुछ कर सकते हैं और नई-नई चीज़ों की खोज करने के क़ाबिल भी हो सकते हैं तो यह नई ज्ञानपरक विधि दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होती चली गई। समय गुज़रने के साथ-साथ पश्चिमवालों में यह प्रवृत्ति आम हो गई कि जो चीज़ अवलोकन और अनुभव में आ सकती है, वही ज्ञान है और जो चीज़ अवलोकन और अनुभव में नहीं आती वह ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान से मुराद मात्र विज्ञान और अनुभवी ज्ञान होता तो ज़्यादा आपत्तिजनक बात नहीं थी, लेकिन चूँकि पश्चिम में ज्ञान और विज्ञान दोनों पर्यायवाची हो गए। यानी अनुभवों पर आधारित ज्ञान और अनुभवहीन ज्ञान दोनों पर्याय बन गए हैं। इसलिए यह ग़लत-फ़हमी बहुत आसानी से उनके यहाँ पैदा हो गई। उसके बाद जब उन्होंने यह देखा कि जिन वैज्ञानिक या बौद्धिक खोजों को उन्होंने अपनी ज्ञानपरक विधि या ‘इस्तिक़राई-मंतिक़’ के आधार पर सच माना था, वे बहुत जल्द ग़लत या विचारणीय साबित हुए तो बजाय इसके कि वे अपनी इस विधि पर पुनरीक्षण करते, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि सत्य और सच्चाई मात्र अतिरिक्त चीज़ें हैं। किसी वास्तविक सत्य का या शाश्वत सच्चाई का कोई अस्तित्व नहीं। निश्चित ज्ञान दुनिया में पाया ही नहीं जाता। यह जितने ज्ञान और कलाएँ हैं ये सब प्रयोगात्मक (tentative) हैं, उनकी सत्यता मात्र अस्थायी और अतिरिक्त है। यही वजह है कि जब इस दृष्टिकोण से अक़ीदे को देखा जाएगा तो अक़ीदा उनको dogma ही मालूम होगा। यही वजह है कि जो चीज़ अक़ीदे पर आधारित हो उसको वे dogmatic क़रार देकर नज़रअन्दाज़ करने या उसका महत्त्व कम करने की कोशिश करते हैं।
इसके मुक़ाबले में मुसलमान चिन्तकों ने पहले दिन से इस तरह का कोई विभाजन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ज्ञान के साधनों को मात्र अनुभव एवं अवलोकन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यह बताया कि ज्ञान के साधन मौलिक रुप से तीन हैं। इन्हीं तीन साधनों के आधार पर इस्लामी विद्वानों ने अपनी तमाम बहसों को बयान किया है। ये तीन साधन ये हैं—(1) इंसान की इन्द्रियाँ (2) सच्ची ख़बर देनेवाले की ख़बर (3) मानव बुद्धि, इन तीनों माध्यमों से इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है।
अनुभव की रौशनी में देखा जाए तो आज भी इंसान इन्हीं तीनों साधनों से ज्ञान प्राप्त करता है। जिस आदमी के बारे में यह विश्वास हो जाए कि यह सच्चा है और सच बात कह रहा है उसकी बात को बेधड़क आज भी मान लिया जाता है। इंसानों के 99 प्रतिशत मामलात इसी आधार पर चलते हैं। आज की दुनिया विज्ञान पर ईमान रखने का दावा करती है। जिस समाज में जिस भीड़ में जाकर देखें, वहाँ वैज्ञानिकों के कथन अन्तिमि निर्णय का दर्जा रखते हैं। लेकिन अगर किसी से यह पूछें कि जो वैज्ञानिक ये सब कुछ कहते हैं वे वैज्ञानिक कौन हैं?
क्या आपसे सचमुच किसी नोबल लारी एट फिज़िक्स के माहिर वैज्ञानिक ने आकर कहा है कि अमुक-अमुक बात विज्ञान में इस तरह होती है? या विज्ञान के शोध के अनुसार अमुक बात यों होती है? सच तो यह है कि एक लाख में से निन्यानवे हज़ार नौ सौ निनानवे (99999) इंसानों ने मात्र विज्ञान से प्रभावित और वैज्ञानिकों पर अन्धे भरोसे की वजह से विज्ञान से जुड़ी बहुत-सी बातें यों ही मान ली हैं। और अगर किसी ने ख़ुद शोध किया है तो वह लाखों में एक ही आदमी है। लेकिन उमूमी तौर पर लोग अस्पष्ट (vague) अन्दाज़ में बयान करते हैं कि विज्ञान ने यह साबित कर दिया है और वह साबित कर दिया है। जो आदमी यह बात कह रहा होता है अगर उसको आप सच्चा आदमी समझते हैं और उसके बयान पर भरोसा करते हैं तो इस भरोसे के आधार पर इस बात को सही मान लेते हैं। गोया अस्ल (actual ) सत्य यह है कि हमारी प्रतिदिन की ज़िन्दगी में जो चीज़ हर वक़्त पेश आती है वह यह है कि इंसान एक सच्चे ख़बर देनेवाले की ख़बर पर एक बात को सही स्वीकार कर लेता है।
इस तरह के हज़ारों, लाखों मामले और घटनाएँ और बयानात इंसानों के ज्ञान में हैं जिनको इंसान वास्तविकता मानता है और जो दरअस्ल कभी भी उसके अवलोकन और निजी अनुभव में नहीं आए। न ही निजी रूप से उसने अपनी बुद्धि से उनकी खोज की, बल्कि मात्र किसी ख़बर देनेवाले ने उसको ख़बर दी। हममें से बहुत-से लोग शायद ब्राज़ील कभी नहीं गए। उसके बावजूद हम में से हर एक जानता है कि ब्राज़ील के नाम से एक देश है। वहाँ की राजधानी रियो डि जेनेरो है। अर्जेनटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। लेकिन इसे न तो हमने देखा है और न ही विशुद्ध बौद्धिक और तार्किक प्रमाणों से यह बात मालूम हुई है। यह बात मात्र मुख़्बिर की ख़बर देने से मालूम हुई, विशुद्ध बौद्धिक तर्कों के आधार पर ऐसे मामलों का ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसे मामले मुख़्बिर की ख़बर से ही मालूम हो सकते हैं। वह मुख़्बिर पत्रकार हो या भूगोल का जाननेवाला हो, कोई पर्यटक हो, इतिहासकार हो, किसी-न-किसी मुख़्बिर की ख़बर से हमें यह पता चला कि ब्यूनस आयर्स और रियो डि जेनेरो दो शहर हैं जो दक्षिण-अमेरिका में पाए जाते हैं। इसी तरह से आप अपने ज़ेहन में सुरक्षित तथ्यों का जायज़ा लें तो अनगिनत तथ्य आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इंसान तथ्य समझता है, लेकिन दरअस्ल वे कभी भी इंसान के अपने अवलोकन और अनुभव के तराज़ू से साबित नहीं होते, बल्कि वे मात्र मुख़्बिर के ख़बर देने से इंसान के ज्ञान में आते हैं।
ऐसे मुख़्बिर की ख़बर को, जिसके सच्चा होने का हमें यक़ीन या गुमान हो, मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने विशुद्ध ज्ञानपरक अन्दाज़ में बयान किया है। वे यह कहते हैं कि मुख़्बिरे-सादिक़ (सच्चा ख़बरी) वह है जिसकी अमानत और सच्चाई पर आपको पूर्ण विश्वास हो। उसके सच्चे और ईमानदार होने पर विश्वास हो, उसका चरित्र, रवैया और तर्ज़े-अमल इस बारे में इस बात के गवाह हों कि वह सादिक़ (सच्चा) भी है और अमीन (ईमानदार) भी। अगर ऐसा मुख़्बिर कोई ख़बर दे तो आप उसकी बात मान लेते हैं। हमारी आए दिन की ज़िन्दगी में ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। इसलिए मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने जब सच्ची ख़बर को ज्ञान का साधन क़रार दिया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी सच्चाई और सत्यता की एक के बाद एक गवाही असंख्य इंसानों का रवैया दे रहा है।
जिन चीज़ों को अक़ीदा कहा जाता है ये वे हैं जो क़तई और निश्चित रूप से ज्ञान के इन तीनों साधनों से हमारी जानकारी में आई हैं। ये शिक्षाएँ अवलोकन के परिणामस्वरूप ज्ञान में आई हों, जैसे प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के अवलोकन में एक चीज़ आई, या मुख़्बिरे-सादिक़ की ख़बर देने के नतीजे में, जैसे पवित्र क़ुरआन या सुन्नत के द्वारा हमारे सामने आई, या इंसानों ने अपने बुद्धि से एक बात तर्कों के द्वारा मालूम की; या पवित्र क़ुरआन और हदीसों से एक चीज़ निकाली। यही वे बाते हैं जिनसे अक़ीदा साबित होता है।
अक़ीदे की कुछ मौलिक विशिष्टताएँ हैं जो उसको ग़ैर-अक़ीदे से अलग करती हैं। शिक्षाएँ तो क़ुरआन और सुन्नत में बहुत-सी हैं, लेकिन जो चीज़ें अक़ीदे की हैसियत रखती हैं ये वे हैं जो हर प्रकार के परिवर्तन और व्याख्या से सुरक्षित हैं। अक़ीदे में न कोई संशोधन होता है न कोई परिवर्तन। हाँ अक़ीदे को बयान करने की शैली बदल सकती है, अक़ीदे को स्पष्ट रूप से बयान करने का अन्दाज़ बदल सकता है। जैसा कि इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) के विकास के इतिहास से पता चलता है। यूनानी मंतिक़ (तर्कशास्त्र) के प्रभाव से जब चौथी-पाँचवीं शताब्दी के बाद के समयों में अक़ीदों की व्याख्या हो रही थी तो उसका अन्दाज़ और ही था। जब उपमहाद्वीप में बड़े सूफ़ियों मसलन मुजद्दिद अल्फ़-सानी यहाँ के वैचारिक माहौल में अक़ीदों की व्याख्या कर रहे थे तो उनका और अन्दाज़ था, अल्लामा इक़बाल के उर्दू और फ़ारसी लेखों में जिनमें मुख्य रूप से मुसलमानों को सम्बोधित किया गया है, उनका अन्दाज़ और शैली और है। इसके विपरीत उनके अंग्रेज़ी ख़ुतबात Reconstruction में जहाँ उनके सामने मुख्य रूप से पश्चिमवाले या पश्चिमी चिन्तन एवं दर्शन से प्रभावित पूर्वी छात्र हैं उनका अन्दाज़ और है। मौलाना शिबली नोमानी की ‘इल्मुल-कलाम’ का और अन्दाज़ है, मौलाना अशरफ़ अली थानवी का और अन्दाज़ है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का और अन्दाज़ है। अत: वर्णन शैली हर दौर में बदलती रहेगी, लेकिन जो अक़ीदे की आत्मा और वास्तविकता है वह एक ही है और एक ही रहेगी।
यही वजह है कि तमाम इस्लामी फ़ुक़हा का यह सर्वसम्मत दृष्टिकोण है कि अक़ीदे की आयतों और हदीसों में से न तो किसी को स्थगित किया जा सकता है न उनके अर्थों को ख़ास किया जा सकता है। स्थगन और ख़ास करने का कार्य केवल आदेशों में हो सकता है, जहाँ ‘तदरीज’ (क्रमशः) या किसी स्थगन और तत्त्वदर्शिता के सामने पिछले आदेशों में परिवर्तन की ज़रूरत होती है, उदाहरण के रूप में पहले आदेश दिया गया कि एक मुसलमान दस विधर्मियों का मुक़ाबला करे, सौ मुसलमान एक हज़ार का मुक़ाबला करें। बाद में कहा गया कि तुम्हारे अन्दर कमज़ोरी आ गई है अत: दो के मुक़ाबले में एक ज़रूर होना चाहिए। यहाँ एक आदेश है, यह एक अमल है जिसे ख़ास किया जा सकता है। स्थगन भी हो सकता है। पहले कहा गया कि शराब उस समय मत पियो जब नमाज़ के क़रीब जाने लगो। फिर स्थायी रूप से उसको हराम कर दिया गया। यह एक आदेश है जिसमें स्थगन भी हो सकता है और ख़ास भी किया जा सकता है। अक़ीदे में न स्थगन होता है और न परिवर्तन। फिर अक़ीदा एक क़तई और निर्धारित चीज़ होती है। वह कोई अस्पष्ट और अनिर्धारित चीज़ नहीं होती। अक़ीदे में कोई विकास नहीं। आदेश में विकास होता रहता है। आदेश में एक आदेश से दूसरा आदेश है, दूसरे से तीसरा निकलता है, तीसरे से चौथा निकलता है और यों फ़िक़्ह और फ़तावा के नए-नए दफ़्तर संकलित होते रहते हैं। इज्तिहाद के नमूने आए दिन सामने आते रहते हैं।
अक़ीदे में इस तरह का कोई विकास नहीं होता, इसलिए कि जिन तथ्यों को मानने का नाम अक़ीदा है वे तथ्य वही हैं और वही रहेंगे जो पवित्र क़ुरआन और हदीस के नुसूस (स्पष्ट आदेशों) में बयान किए गए हैं। अक़ीदे में सार्वजनिकता का रंग पाया जाता है और व्यापकता पाई जाती है। ऐसी सार्वजनिकता और व्यापकता जो समय और जगह से परे हो। फिर इस्लाम के अक़ीदों में बुद्धि और नक़्ल के मध्य पूर्ण समरसता और परिपूर्णता पाई जाती है। जो अक़ीदे लिखे हुए हैं, बुद्धि उनकी पूर्ति करती है। जो सीमाएँ बुद्धि ने खोजी हैं, लिखे हुए से उनका समर्थन होता है। इसलिए बुद्धि और समर्थन में पूर्ण समरसता भी अक़ीदे का अनिवार्य अंग है।
बुद्धि एवं नक़्ल में मेल-मिलाप के विषय पर इस्लाम के बहुत-से बड़ों ने क़ाबिले-क़द्र इल्मी और वैचारिक काम किया है। इमाम ग़ज़ाली, इमाम राज़ी, इब्ने-रुश्द और अल्लामा इब्ने-तैमियाः के नाम मुतक़द्दिमीन (आरम्भ के विद्वानों) में और शैख़ुल-इस्लाम मुस्तफ़ा सबरी, मौलाना अशरफ़ अली थानवी वग़ैरा के नाम मुताख़्ख़िरीन (बादवाले विद्वानों) में इस मामले में बहुत नुमायाँ हैं। फिर चूँकि मुसलमान दूसरे धर्मों के विपरीत पैग़म्बरी समाप्त हो जाने के अक़ीदे पर ईमान रखते हैं इसलिए भी अक़्ल और नक़्ल (बुद्धि एवं धर्मग्रन्थों में लिखे सिद्धान्तों) का एक-दूसरे से मेल खाना उनके अक़ीदे और ईमान की अनिवार्य अपेक्षा है। ख़त्मे-नुबूवत (पैग़म्बरों का सिलसिला समाप्त हो जाने) पर ईमान का अर्थ यह है कि अब अल्लाह की ओर से वह्य अवतरित होने का सिलसिला बन्द हो गया। अब वह्य (अर्थात् क़ुरआनी आदेशों) की रौशनी में शरीअत की सीमाओं के अन्दर इज्तिहाद कर के ही आगे के तमाम मामलात तय होंगे। आइन्दा मानव-बुद्धि की भूमिका एक मौलिक महत्त्व रखती होगी। अतीत में तो नई समस्याओं के हल के लिए नए पैग़म्बर की प्रतीक्षा की जा सकती था, लेकिन अब ख़ुद आम इंसानों को इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। यही वजह है कि ‘इज्तिहाद’ और ‘इजमा’ की संस्थाएँ इतने संगठित ढंग से और इतने परिपूर्ण रूप में इस्लामी फ़िक़्ह में बयान की गईं कि अतीत के किसी धर्म में इसका उदाहरण नहीं मिलता। यहूदियों के यहाँ ‘इजमा’ से मिलती-जुलती चीज़ मौजूद है, लेकिन इज्तिहाद और इजमा की संस्थाओं की जो भूमिका इस्लाम के इतिहास में रही है और विशेष रूप से इज्तिहाद की जो भूमिका है उसकी कोई मिसाल किसी और धर्म में नहीं मिलती। इसलिए कि इज्तिहाद और ख़त्मे-नुबूवत दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। ख़त्मे-नुबूवत की माँग है कि इज्तिहाद हो और इज्तिहाद को तार्किक औचित्य और शरई दर्जा तब ही प्राप्त होगा जब ख़त्मे-नुबूवत पर ईमान होगा। अगर पैग़म्बरी जारी है तो इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं, और अगर पैग़म्बरी ख़त्म हो गई तो इज्तिहाद अनिवार्य है।
ज्ञान के साधनों के सन्दर्भ में कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ज्ञान के केवल दो साधन हैं, एक अल्लाह की वह्य और दूसरी मानव-बुद्धि। यह भी दुरुस्त है। इसलिए कि अवलोकन और अनुभव से अधिक ज्ञानपरक परिणाम निकालनेवाली जो शक्ति है वह मानव-बुद्धि ही है। आप मानव-बुद्धि को एक गिनें या बुद्धि और अवलोकन एवं अनुभव को अलग-अलग गिन लें, यह मात्र वर्णन शैली का अन्तर हो सकता है, लेकिन वास्तविकता एक ही है। दरअसल यह मानव-बुद्धि ही है जो अनुभव और अवलोकन के आधार पर नए-नए निष्कर्ष निकालती है। इमाम अबू-मंसूर मातुरीदी (मृत्यु 333 हिजरी) ने, जो एक बहुत बड़े कलामी मसलक के संस्थापक हैं और अक्सर हनफ़ी उलमा उनके कलामी दृष्टिकोण से सहमत हैं, अल्लाह द्वारा अवतरित वह्य और बुद्धि दोनों को दो बड़े ज्ञान के साधनों के तौर पर बयान किया है। उनका ख़याल है कि अक़ीदा इन्ही दो के आधार पर संकलित होता है।
[यह विचार बिलकुल ग़लत है। इस्लाम के अनुसार अक़ीदे का मूल स्रोत सिर्फ़ और सिर्फ़ वह्य द्वारा अवतरित आदेश अर्थात् क़ुरआन में वर्णित सिद्धान्त हैं, वे सारे परोक्ष सम्बन्धी तथ्य जिनको देखे बिना मानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क़ुरआन में बयान कर दिए गए हैं। इनके अलावा अपनी बुद्धि से कुछ और अक़ीदे बना लेना न केवल इस्लाम की नज़र में ग़लत है, बल्कि इससे शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। सूफ़ियों से यही ग़लती हुई कि उन्होंने अपनी अनुभूतियों को अक़ीदा बना लिया और इस प्रकार इस्लामी अक़ीदों में बहुत-सी इस्लाम विरोधी चीज़े शामिल कर लीं, जो तसव्वुफ़ के माननेवालों में आज भी फैली ही———अनुवादक]
अक़ीदा जिसके महत्त्व के बारे में विस्तार से बताया गया, पवित्र क़ुरआन के अनुसार यह एक स्वाभाविक अपेक्षा है, हर इंसान जो सद्बुद्धि रखनेवाला है, दीन-पसन्द है, दीनी प्रवृत्तियाँ रखनेवाला है, वह सद्बुद्धि पर क़ायम है। पवित्र क़ुरआन ने यह बताया है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से सद्बुद्धि रखनेवाला है, भली प्रवृत्ति का है, दीन-पसन्द है और धार्मिक प्रवृत्तियों का ध्वजावाहक है। इंसान का इतिहास यही बताता है कि इंसान हर दौर में दीनी अक़ीदों और दीनी मूल्यों पर कार्यरत रहा है। आज भी विशुद्ध अधर्मिता और विशुद्ध नास्तिकता अपवाद की हैसियत रखते हैं। मानव इतिहास नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस एलान की गवाह और समर्थक है जिसमें उन्होंने फ़रमाया कि “हर नया पैदा होनेवाला बच्चा स्वाभाविक प्रकृति पर पैदा होता है।” पवित्र क़ुरआन में इसी स्वाभाविक प्रकृति की ओर इशारा करते हुए कहा गया “यह अल्लाह की पैदा की हुई वह फ़ितरत है जिसपर अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया है।” पवित्र क़ुरआन की अनेक आयतों और बहुत-सी हदीसों में इस विषय को विभिन्न ढंग और विभिन्न पहलुओं से बयान किया गया है।
इस्लामी चिन्तकों ने विशुद्ध बौद्धिक तर्कों से भी यह बात स्पष्ट की है कि अक़ीदा इंसान की मौलिक आवश्यकता है। दीन के अक़ीदे, दीन की शिक्षा और दीनी मूल्य स्वाभाविक रूप से इंसानों की ज़रूरत हैं। जिस तरह सृष्टि में भौतिक रिक्तता सम्भव नहीं है, उसी तरह वैचारिक रिक्तता भी सम्भव नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने अपने प्रसिद्ध अभिभाषण ‘क्या मज़हब मुम्किन है?’ में यही बात अत्यन्त गहन चिन्तन और बौद्धिक रूप में कही है। इस्लामी चिन्तक इंसान को सामूहिक पशु, नागरिक पशु, राजनैतिक पशु और चिन्तक पशु क़रार देते आए हैं। जहाँ तक सामूहिक पशु होने का सम्बन्ध है तो यह बात बहुत प्राचीनकाल से कही जा रही है, अफ़लातून और अरस्तू के ज़माने से इंसान को सामूहिक पशु कहा जा रहा है। इस्लामी चिन्तकों ने इंसान को राजनैतिक पशु, चिन्तक पशु और नागरिक पशु भी क़रार दिया। लेकिन अगर इंसान यह सब कुछ है तो फिर इंसान दीनदार पशु भी है। इस बात को बहुत विस्तार के साथ अनेक विद्वानों ने बयान किया है जिनमें एक नुमायाँ नाम जैसा कि मैंने बताया, अल-जज़ाइर के प्रसिद्ध चिन्तक मालिक-बिन-नबी का है, जिन्होंने अपनी किताब ‘अज़-ज़ाहिरतुल-क़ुरआनियः’ में इतिहास, मानव-विज्ञान और दर्शन के हवालों से साबित किया है कि इंसान के इतिहास का अधिकांश भाग धार्मिक मूल्यों के मार्गदर्शन में गुज़रा है और अधर्म एक अपवाद की हैसियत से रहा है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार जो बात अक़ीदा कहलाती है वह अत्यन्त निश्चित और सर्वसम्मत है। तमाम आसमानी किताबों, पैग़म्बरों (अलैहिस्सलाम) की शिक्षा और आकाशीय ईशदूतत्व का इसपर मतैक्य रहा है कि अक़ीदे के मौलिक आधार समान हैं। तौहीद (एकेश्वरवाद), रिसालत (ईशदूतत्व), रोज़े-आख़िरत (परलोक) और दीनी सच्चाइयों पर ईमान, वे धार्मिक तथ्य हैं जिनकी तमाम पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) दावत देते हैं।
अक़ीदे का सुबूत निश्चित और स्पष्ट आदेशों के आधार पर होता है, पवित्र क़ुरआन की स्पष्ट और दोटूक आयतें अक़ीदे का सबसे बड़ा स्रोत हैं, फिर वे प्रमाणित हदीसें जो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से निश्चित रूप से सिद्ध हैं जिनके सुबूत में कोई मतभेद न रहा हो उनसे भी अक़ीदा साबित होता है [अलबत्ता इन अक़ीदों की हैसियत अतिरिक्त अक़ीदों की है, मूल अक़ीदें जिनपर किसी इनसान के मुसलमान होने या न होने का दारोमदार है, उनका आधार केवल और केवल क़ुरआन है———अनुवादक]
एक बहस एक वर्ग में यह पैदा हो गई है कि ख़बरे-वाहिद यानी वे रिवायतें और हदीसें जिनको बयान करनेवाले किसी सतह पर एक ही व्यक्ति रहे हों उनसे अक़ीदा साबित होता है या नहीं होता। आम मुतकल्लिमीने-इस्लाम यही लिखते चले आए हैं कि ख़बरे-वाहिद से अक़ीदे का सुबूत नहीं होता और ख़बरे-वाहिद के आधार पर साबित होनेवाली कोई शिक्षा अक़ीदे की हैसियत नहीं रखती। आधुनिक काल के कुछ लोगों ने इसपर बहुत ग़ुस्से का इज़हार किया है और बहुत ज़ोर देकर यह बात साबित करने की कोशिश की है कि ख़बरे-वाहिद से भी अक़ीदा साबित होता है।
दरअस्ल इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई टकराव नहीं है, जो लोग यह लिखते चले आए हैं और उनमें इस्लाम के बड़े-बड़े विद्वान शामिल हैं कि ख़बरे-वाहिद से अक़ीदा साबित नहीं होता, उनकी मुराद यह भी नहीं रही कि अक़ीदों के मामले में ख़बरे-वाहिद की कोई हैसियत ही नहीं है और (अल्लाह की पनाह) ख़बरे-वाहिद में जो कुछ बयान किया गया उसको अक़ीदों के मामले में सिरे से नज़र-अन्दाज़ कर दिया जाए। उनकी मुराद इस बात से यह है कि जो मामलात ख़बरे-वाहिद से साबित होते हैं, उनसे अक़ीदे की वज़ाहत भी होती है, अक़ीदे की व्याख्या भी होती है, अक़ीदे के विवरण का भी अन्दाज़ा होता है, लेकिन इन मामलों का दर्जा दीन की आवश्यकताओं का नहीं होता। ऐसी किसी रिवायत को न माननेवाला इस्लाम के दायरे से ख़ारिज नहीं होता। ख़बरे-वाहिद से साबित होनेवाली शिक्षा की क़िस्म दीन की आवश्यकताओं की नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने शोध के आधार पर किसी हदीसे-आहाद या ख़बरे-वाहिद के सुबूत में संकोच करता है और उस हदीस में बयान किए जानेवाली किसी घटना या वास्तविकता के बारे में संकोच करता है तो उसको दीन की आवश्यकताओं का इनकार करनेवाला नहीं कहा जाएगा और वह इस्लाम के दायरे से ख़ारिज नहीं होगा। इसके विपरीत वे मामले जो पवित्र क़ुरआन के स्पष्ट आदेशों से साबित हैं और प्रमाणित हदीसों और मुतवातिर हदीसों से साबित हैं, उनका इनकार करनेवाला दीन की आवश्यकताओं का इनकारी समझा जाएगा और दीन की आवश्यकताओं का इनकार इंसान को इस्लाम के दायरे से ख़ारिज कर सकता है। इसलिए यह मात्र एक शाब्दिक मतभेद है, वास्तव में यह कोई मौलिक मतभेद नहीं है।
इस बात पर भी तमाम इस्लामी विद्वानों का मतैक्य है कि अक़ीदे के मामलात आरम्भ से एक ही रहे हैं, अक़ीदे में न कोई संशोधन हुआ है न कोई अक़ीदा स्थगित हुआ है और न अक़ीदों के मामले में कोई परिवर्तन हो सकता है। अक़ीदे हर प्रकार के फेर-बदल और परिवर्तन से सुरक्षित हैं, पवित्र क़ुरआन का टेक्स्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सुन्नते-साबिता (प्रमाणित हदीसों) के टेक्स्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, इसलिए इस्लामी अक़ीदा निर्धारित, निश्चित और तय-शुदा है, यहाँ यहूदियत या ईसाइयत या दूसरे धर्मों की तरह कोई ऐसी अथॉरिटी या प्रमाण मौजूद नहीं है जो अक़ीदों के मामले में फेर-बदल करती रहे, यह अक़ीदा एक उमूमी शान रखता है, उन तमाम मामलात को समेटे हुए है जो अक़ीदे में शामिल होने चाहिएँ, अक़्ल और नक़्ल में पूर्ण सन्तुलन पर आधारित है। अक़ीदे के मामलात में यह तो हो सकता है कि पवित्र क़ुरआन या सुन्नत ने किसी वास्तविकता को इंसानों के ज़ेहन से क़रीब करने के लिए उसको मुतशाबिहात (उपलक्षित आयतों) के अन्दाज़ में, अलंकारों और सांकेतिक शैली में बयान किया हो, लेकिन जितना हिस्सा पवित्र क़ुरआन या सुन्नत से निश्चित रूप से साबित है उसको ज्यों-का-त्यों मानना मुसलमान होने के लिए अनिवार्य है। यह तो सम्भव है कि किसी अलंकार या प्रतीक की व्याख्या में विद्वानों के मध्य मतभेद हो, लेकिन जितना हिस्सा पवित्र क़ुरआन या हदीसों में बयान हुआ है उसको मानना, उसको वास्तविकता और निश्चितता पर आधारित समझना यह मुसलमान होने लिए अनिवार्य है। इसके मुक़ाबले में जिसको ग़ैर-मुस्लिमों का अक़ीदा कहा जाता है यह एक आन्तरिक विवेक का नाम है जिसका आधार मात्र भावनाएँ और अनुभूतियाँ या अन्धविश्वास तथा ख़ुराफ़ात पर है, जिन मामलात को दूसरी क़ौमों में अक़ीदे का दर्जा प्राप्त है उनमें भावनाएँ, अनुभूतियाँ, क़िस्से, कहानियाँ, किवदंतियाँ और किसी हद तक बौद्धिक मामलात भी शामिल हैं।
[दिलचस्प बात है कि यही लेखक महोदय ऊपर की पंक्तियों में अबू-मंसूर मातुरीदी के हवाले से यह कह चुके हैं कि अक़ीदे के आधार दो हैं—(1) अल्लाह द्वारा अवतरित वह्य अर्थात् क़ुरआन (2) इंसान की बुद्धि। मगर यहाँ ये ख़ुद मातुरीदी साहब के सिद्धान्त का खंडन करते हुए यह बता रहे हैं कि बुद्धि अक़ीदे का आधार नहीं बन सकती और यह कि बुद्धि को अक़ीदे का आधार मानना दूसरे धर्मों की रीति रही है, इस्लाम की नहीं——अनुवादक]
जिन लोगों ने दूसरे धर्मों में अक़ीदे की परिभाषा की है उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से बयान की है कि अक़ीदे का प्रमाण पर आधारित होना या बुद्धि पर आधारित होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बात इतनी गहरी भावनाओं पर आधारित हो कि जनसाधारण उसको मानते हों या जनसाधारण की बड़ी संख्या उसको सही समझती हो तो यह बात अक़ीदा होने के लिए काफ़ी है। प्रसिद्ध पश्चिमी फ़लसफ़ी डेकार्ट ने अक़ीदे के बारे में कहा है कि दरअस्ल यह यों तो मौलिक रूप से मानव-बुद्धि पर आधारित है, लेकिन अधिकांश इसका सम्बन्ध इंसान के इरादे से है, इंसान जिस चीज़ को मानना चाहता है वह उसका अक़ीदा कहलाती है। कुछ और पश्चिमी चिन्तकों ने अक़ीदे से मुराद राय ली है। उनके ख़याल में यह एक राय है जिसे कुछ लोग दुरुस्त मानते हैं और कुछ लोग दुरुस्त नहीं मानते। जैसा कि मैंने पहले बताया, अक़ीदों को बहुत-से पश्चिमी लोग एक राय समझते हैं जिसका सत्य पर आधारित होना ज़रूरी नहीं, कुछ की राय में यह दुरुस्त है और कुछ की राय में सही नहीं है। इसके विपरीत इस्लामी अक़ीदे के अनुसार, इस्लाम के अक़ीदे क़तई और निश्चित रूप से सत्य हैं और सत्य उनमें निहित है, जो चीज़ उनके अनुसार है वह सत्य है, जो उनसे टकराती है वह उनसे टकराव की हद तक असत्य है।
अक़ीदे के बारे में इस्लामी चिन्तकों ने लिखा है कि जनसाधारण की यह ज़िम्मेदारी है कि अपनी बुद्धि से काम लें और चिन्तन-मनन से काम लेकर अक़ीदे की मौलिक और आधारभूत बातों पर ईमान रखें, चुनाँचे तौहीद पर ईमान, तमाम इस्लामी चिन्तकों के नज़दीक इंसानियत की अनिवार्य अपेक्षा है जिसके लिए पैग़म्बरी और रिसालत की शिक्षा का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। चुनाँचे अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए पैग़म्बरी का सन्देश नहीं पहुँचा, रिसालत की शिक्षा उस तक नहीं पहुँची तो वह अल्लाह ने चाहा तो आख़िरत में मुक्ति पा लेगा अगर वह दीन के विवरण से अनभिज्ञ रहे और उनपर अमल न कर पाए, लेकिन अगर वह तौहीद (एकेश्वरवाद) पर ईमान न लाए, सृष्टि के रचयिता के अस्तित्व को स्वीकार न करे तो उसका यह बहाना स्वीकार्य नहीं होगा कि उसको दीनी शिक्षा नहीं पहुँची थी। इसलिए कि अल्लाह तआला की पहचान जिन गवाहियों और तर्कों से प्राप्त हो सकती है, वह इस सृष्टि में मौजूद हैं और सृष्टि के इन तथ्यों एवं सुबूतों को समझने और उनको महसूस करने के लिए अल्लाह तआला ने हर इंसान को बुद्धि दी है जिसके आधार पर वह इन गवाहियों के द्वारा अल्लाह तआला की पहचान तक पहुँच सकता है।
यह बात मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने ही नहीं लिखी, मुतकल्लिमीन, सूफ़ियों, उलमाए-उसूल और यहाँ तक कि मुस्लिम दार्शनिकों ने भी लिखी है। इब्ने-रुश्द ने बहुत विस्तार से यह बात बयान की है कि अल्लाह तआला की पहचान ज़रूरी और अनिवार्य है, ‘मारिफ़ते-कामिला’ (पूरी पहचान) के लिए ‘दलील’ और ‘बुरहान’ से जानकारी दरकार है, ‘दलील’ और ‘बुरहान’ के लिए ज़रूरी है कि इंसान यह ज्ञान भी प्राप्त करे कि ‘दलील’ और ‘बुरहान’ कहते किसको हैं, ‘दलील’ और ‘बुरहान’ की शर्तें क्या हैं? ये शर्तें इब्ने-रुश्द के नज़दीक ‘क़ियास’ और ‘मंतिक़’ की जानकारी हैं। ‘क़ियास’ की जानकारी के लिए ज़रूरी है कि इंसान ‘क़ियास’ की क़िस्में यानी ‘क़ियासे-बुर्हानी’, ‘क़ियासे-जदली’ और ‘क़ियासे-ख़िताबी’ से अच्छी तरह अवगत हो। इन मामलों के लिए मंतिक़ (तर्कशास्त्र) और अक़ल्लियात (बुद्धि शास्त्र) का जानना ज़रूरी है।
यह बात इमाम ग़ज़ाली, इब्ने-रुश्द और बहुत-से दूसरे इस्लामी दार्शनिक लिखते चले आए हैं कि प्रचलित अक़ल्लियात से जानकारी मुसलमानों के ज़िम्मे फ़र्ज़े-किफ़ाया है। इसलिए कि शरीअत ने मौजूद चीज़ों पर, सृष्टि पर बौद्धिक दृष्टि डालने और सबक़ सीखने का आदेश दिया है। जिसको शरीअत में ‘एतिबार’ या ‘इबरत प्राप्त करना’ कहा गया है, वह मालूम चीज़ से नामालूम चीज़ का आदेश मालूम करना है। इसी को ‘क़ियास’ कहते हैं। अत: इस्लामी दार्शनिकों के नज़दीक क़ियास, तर्कशास्त्र और बौद्धिकता का ज्ञान अनिवार्य है। इब्ने-रुश्द ने इस सन्दर्भ में पवित्र क़ुरआन की उन आयतों का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐ बुद्धिवालो इबरत प्राप्त करो। क्या ये लोग ज़मीन-आसमान की बादशाहत में सोच-विचार नहीं करते? क्या उन लोगों ने अमुक-अमुक प्राणियों को नहीं देखा? क्या उन्होंने ज़मीन-आसमान में ग़ौरो-फ़िक्र नहीं किया? और इस तरह की अनगिनत आयतें हैं जिनमें चिन्तन-मनन और सोचने का आदेश दिया गया है और यह चिन्तन-मनन और सोच अल्लाह के अस्तित्व की जानकारी और तौहीद के अक़ीदे तक पहुँचने के लिए काफ़ी है। अक़ीदे और कलाम पर लिखनेवाले विद्वानों ने अक़ीदे की महत्त्वपूर्ण बहसों और विषयों को चार अहम शीर्षकों के तहत विभाजित किया है।
- इलाहियात
- नबवात
- कौनियात
- ग़ैबियात
आंशिक रूप से यह विभाजन या इससे मिलते-जुलते विभाजन प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये शब्दावलियाँ भी लगभग इब्ने-सीना के ज़माने से प्रयोग हो रही हैं। चार बहसों का यह विभाजन समझने और आसानी के लिए है, इन शीर्षकों के तहत अक़ीदे और कलाम के महत्त्वपूर्ण बहसें बयान की गई हैं। उनमें वे बहसें भी शामिल हैं जिनसे अक़ीदे और कलाम की बहसों का दूसरी तीसरी शताब्दी हिजरी में आरम्भ हुआ। एक प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान ने जिसने इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) पर अनेक किताबें लिखी हैं और जो पश्चिम में कलाम पर लिखनेवाले प्राच्यविदों में अत्यन्त नुमायाँ समझा जाता है, प्रोफ़ेसर हैरी एफ़ ऑल्सन (Harry F. Olson) ने लिखा है कि इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की मौलिक समस्याएँ छः हैं। मसला-ए-सिफ़ात (यानी अल्लाह के गुण क्या हैं), मसला-ए-ख़ल्क़े-क़ुरआन (यानी क़ुरआन अल्लाह का गुण है या अन्य रचनाओं की तरह मात्र एक रचना), ख़ल्क़े-आलम (संसार की रचना), असबाबो-इलल (कारण), जबरो-क़द्र (यानी इंसान मात्र कठपुतली है या उसे कुछ भी करने का अधिकार है), आदि का मसला। इसके यह अर्थ नहीं है कि इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) में केवल यही कुछ समस्याएँ हैं, बल्कि सम्भवतः विद्वान प्राच्यविद् का कहना यह है कि ये समस्याएँ वे महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनसे इल्मे-कलाम में मौलिक रूप से बहस हुई है और जो इल्मे-कलाम की महत्त्वपूर्ण समस्याएँ हैं।
अक़ीदा और ईमानियात की बहसों में सबसे पहली बहस ख़ुद ईमान की है कि ईमान क्या है? ईमान की वास्तविकता के बारे में पहले रोज़ से यह बहस जारी है। दूसरी शताब्दी हिजरी के आरम्भ से, जब से अक़ीदा और ईमान की समस्याओं पर बहस शुरू हुई तो ईमान का महत्त्वपूर्ण मसला भी ज़ेरे-बहस आया। मौलिक सवाल यह था कि क्या आमाल मसलन नमाज़, रोज़ा या ज़कात, यह ईमान की वास्तविकता में दाख़िल हैं या ईमान की वास्तविकता से बाहर हैं। अगर ये ईमान की वास्तविकता में दाख़िल हैं तो फिर ईमान कमो-बेश भी हो सकता है, इसलिए कि किसी के आमाल ज़्यादा होते हैं, किसी के आमाल कम होते हैं। बहुत-से बदनसीब ऐसे भी हैं जो आमाल से बिलकुल अनजान हैं। तो क्या इसी दृष्टि से ईमान में भी कमी-बेशी होती है? इस मसले को बयान करने की दो बड़ी-बड़ी शैलियाँ सामने आईं, एक शैली मुहद्दिसीन लोगों ने अपनाई जिसमें सबसे नुमायाँ नाम अमीरुल-मिमिनीन फ़िल-हदीस हज़रत इमाम बुख़ारी (रह॰) का है। उन्होंने विभिन्न हदीसों को सामने रखते हुए यह राय क़ायम की कि आमाल ईमान में दाख़िल हैं और ईमान में कमी-बेशी हो सकती है। दूसरी राय इमाम अबू-हनीफा (रह॰) ने अपनाई, उनका कहना यह है कि आमाल ईमान की वास्तविकता में दाख़िल नहीं हैं और ईमान में कमी-बेशी नहीं हो सकती। बज़ाहिर ये दोनों रायें आपस में टकराती मालूम होती हैं। बज़ाहिर इन दोनों में कोई समानता नज़र नहीं आती, लेकिन वास्तव में इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। जब इमाम बुख़ारी और उनके समविचार विद्वान यह बयान करते हैं कि आमाल ईमान में दाख़िल हैं और ईमान में कमी-बेशी हो सकती है तो उनकी मुराद यह होती है कि ईमाने-कामिल (पूर्ण ईमान) अच्छे कर्मों के बिना प्राप्त या साबित नहीं होता। यह बात बहुत-सी हदीसों में भी बयान हुई है जिससे यह पता चलता है कि पूरा और वास्तविक ईमान वही है जिसका नतीजा अच्छे कर्मों के रूप में निकले। अगर भले कर्मों का अस्तित्व नहीं है तो इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि ईमान की दौलत पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। फिर जब इमाम बुख़ारी यह कहते हैं कि ईमान में कमी-बेशी होती है तो यह कमी-बेशी इस अर्थ में नहीं होती जिसमें इमाम अबू-हनीफ़ा कमी-बेशी न होने की बात कहते हैं, बल्कि यह कमी-बेशी शिद्दत में, कैफ़ियत में, गहराई में होती है। ईमान में शिद्दत भी पैदा होती है, ईमान कभी-कभी कमज़ोर होता है, कुछ लोगों का ईमान अत्यन्त मज़बूत और पुख़्ता होता है, कुछ का ईमान कमज़ोर होता है। फिर जैसे-जैसे इंसान अच्छे कर्मों का पाबन्द होता जाता है, जैसे-जैसे अल्लाह के डर की कैफ़ियत पुख़्ता होती जाती है ईमान में शिद्दत और परिपक्वता पैदा होती जाती है। यह देखने में आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इमाम बुख़ारी (रह॰) की यह राय बिलकुल दुरुस्त है कि ईमाने-कामिल की कैफ़ियत में शिद्दत और शक्ति में कमी-बेशी होती रहती है।
दूसरी तरफ़ इमाम अबू-हनीफा (रह॰) ने ईमान के मामले को विशुद्ध क़ानूनी और फ़िक़ही दृष्टिकोण से देखा। इमाम साहब की क़ानूनी गहरी नज़र का मुक़ाबला नहीं किया जा सकता। मानव इतिहास के अगर वे सबसे बड़े क़ानूनी दिमाग़ नहीं थे तो कुछ महानतम क़ानूनी दिमाग़ों में उनकी गणना निश्चय ही होती है। वे हर मामले को विशुद्ध क़ानून और फ़िक़्ह के तराज़ू में देखते और तौलते थे। उन्होंने सवाल यह उठाया कि ईमान की वास्तविकता या ईमान का सबसे कम दर्जा क्या है जो ईमान के लिए अनिवार्य है, वह न हो तो ईमान मौजूद नहीं होगा, उतना दर्जा मौजूद हो तो ईमान मौजूद होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इमाम साहब की राय बिलकुल सत्यता पर आधारित है कि आमाल ईमान की वास्तविकता में शामिल नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति आज इस्लाम क़बूल कर ले, दिल से पुष्टि कर ले, या ज़बान से इक़रार कर ले और यह घटना सुबह आठ बजे घटित हो और किसी इत्तिफ़ाक़ के नतीजे या अल्लाह की मशीयत के अनुसार ज़ुहर की नमाज़ से पहले-पहले उसका इन्तिक़ाल हो जाए, तो क्या उस व्यक्ति को मोमिन क़रार दिया जाएगा? इस व्यक्ति ने कोई अमल नहीं किया, कोई नमाज़ नहीं पढ़ी कोई रोज़ा नहीं रखा तो क्या यह मोमिने-कामिल नहीं था, यक़ीनन यह मोमिने-कामिल था। इसका साफ़ अर्थ यह है कि इमाम अबू-हनीफ़ा की राय कि आमाल ईमान की वास्तविकता में शामिल नहीं हैं बिलकुल दुरुस्त है। इसमें किसी शक-सन्देह की गुंजाइश नहीं।
[इस मिसाल से बिल्कुल ग़लत नतीजा निकाला गया है। जिस व्यक्ति को कोई नेक अमल करने की मोहलत ही न मिली हो और वह व्यक्ति जिसे पूरी ज़िन्दगी मोहलत मिले और फिर भी वह अपने ईमान के अनुसार अमल न करे, दोनों में बहुत फ़र्क़ है। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। पहले को अपना ईमान साबित करने का मौक़ा ही नहीं मिला, जबकि दूसरे ने अपने अमल से अपने ईमान के दावे के ख़िलाफ़ व्यावहारिक सुबूत पेश किया। ऐसे में दोनों को एक-जैसा कैसे कहा जा सकता है———अनुवादक]
फिर ऐसे बहुत-से मुसलमान हैं जो अमल में अत्यन्त कमज़ोर हैं, जो नेक आमाल करने में अत्यन्त सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन हदीसों में या पवित्र क़ुरआन में उनको मोमिन के लक़ब से याद किया गया है। पवित्र क़ुरआन की दर्जनों आयात हैं जिनमें एक गुनहगार साहिबे-ईमान को मोमिन के लक़ब से याद किया गया है। अगर आमाल की कमी ईमान का इनकार होता तो ऐसे लोगों को मोमिन के लक़ब से याद न किया जाता। इसी तरह से जब इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) यह फ़रमाते हैं कि ईमान में कमी-बेशी नहीं हो सकती तो उनकी मुराद ईमान की कैफ़ियत या शिद्दत में कमी-बेशी नहीं होती, बल्कि उनकी मुराद ईमान की वास्तविकता में कमी-बेशी होती है। क्या ईमान की जो वास्तविकता या दायरा है, क़ानूनी दृष्टि से जो ईमान की सीमाएँ हैं उसमें कमी हो सकती है? बिलकुल नहीं हो सकती। जिन चीज़ों पर ईमान लाना अनिवार्य है उसमें एक कण-भर कमी होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा, उसमें इज़ाफ़ा भी नहीं हो सकता। जिस चीज़ पर ईमान लाने का शरीअत ने माँग नहीं की उसको आदमी ईमान की वास्तविकता में दाख़िल करेगा तो शरीअत में वृद्धि का मुजरिम होगा जो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से न ईमान में कमी हो सकती है न ज़्यादती हो सकती है।
ख़ुलासा यह है कि ईमान की वास्तविकता ज़बान से इक़रार और दिल से पुष्टि है। आमाल ईमान की अस्ल वास्तविकता में शामिल नहीं हैं, लेकिन ईमान की पूर्ति के लिए अनिवार्य हैं। ईमान की अनिवार्य अपेक्षा यह है कि अच्छे कर्मों के रूप में इसका नतीजा ज़ाहिर हो। ईमान की कम-से-कम क़ानूनी वास्तविकता और कम-से-कम क़ानूनी अपेक्षा वह है जो मुसलमान होने के लिए अनिवार्य है। इसमें न कमी हो सकती है न वृद्धि हो सकती है। हनफ़ी फ़ुक़हा की इस राय पर मुहद्दिसीन के क्षेत्रों में कई बार आलोचना हुई, ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह॰) की किताब सहीह बुख़ारी में इस तरफ़ इशारे मौजूद हैं, लेकिन अगर इस स्पष्टीकरण को सामने रखा जाए जो पेश किया गया तो दोनों रायों में कोई टकराव नहीं रहता और दोनों अपनी-अपनी जगह दुरुस्त हैं।
[इमाम अबू-हनीफ़ा (रह॰) की यह राय कि अमल ईमान का हिस्सा नहीं है और यह कि ईमान घटता-बढ़ता नहीं है, उपर्युक्त स्पष्टीकरण की रौशनी में सही सिद्ध होती है या नहीं, यह हम पाठकों पर छोड़ते हैं। मगर इतना ज़रूर है कि फ़िक़्हे-हनफ़ी की इस राय ने मुसलमानों को बेअमल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज कितने ही मुसलमान हैं, जो इस्लाम के किसी आदेश पर अमल नहीं करते, मगर इस ख़ुशफ़हमी में जीते हैं कि चूँकि उन्होंने ज़िन्दगी में एक बार कलिमा पढ़कर ईमान का इक़रार कर लिया है, इसलिए अब उनका ईमान मुकम्मल है, उसमें कमी-बेशी नहीं हो सकती, चाहे वे इस्लाम पर अमल करें या न करें, कलिमा पढ़कर मोमिन हो जाने की वजह से वे अनिवार्य रूप से जन्नत के हक़दार बन चुके हैं।———अनुवादक]
एक और सवाल यह पैदा हुआ कि क्या ईमान और इस्लाम दोनों का अर्थ एक है। पवित्र क़ुरआन की कुछ आयतों से मालूम होता है कि ईमान और इस्लाम एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सूरा-51 ज़ारियात में एक जगह जहाँ स्ताईसवाँ पारा शुरू होता है वहाँ मोमिनीन और मुस्लिमीन के शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इसके आधार पर कुछ विद्वानों का आग्रह है कि ईमान और इस्लाम दोनों के अर्थ एक हैं। पवित्र क़ुरआन में एक-दूसरे सन्दर्भ में सूरा-49 हुजुरात में ईमान और इस्लाम दो अलग-अलग अर्थ में बयान हुए हैं। एराब और बद्दुओं का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि यह कहते हैं कि हम ईमान ले आए, पवित्र क़ुरआन में बताया गया, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहलवाया गया कि आप उन्हें कह दीजिए कि तुम इस्लाम ले आए लेकिन अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाख़िल नहीं हुआ। इस आयत के आधार पर कुछ विद्वानों का ख़याल है कि ईमान से मुराद दिल की गहराइयों से सच्चाई और वास्तविकता की पुष्टि करना और इस्लाम के अक़ीदों को दिल से मानना और फिर ज़बान से उसका इक़रार करना। इस्लाम से मुराद है ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के आदेशों के सामने सिर झुका देना, चाहे वास्तविकता में दिली पुष्टि मौजूद हो या न हो। इस दृष्टि से ये दोनों अलग-अलग शब्दावलियाँ हैं। यह बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि शब्दावली में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हर ज्ञानवान को अधिकार है कि अपनी शब्दावली तैयार करे और अपनाए। अगर पवित्र क़ुरआन में ये दोनों शब्द इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं तो इस बात की निश्चय ही गुंजाइश मौजूद है कि इन दोनों शब्दावलियों को दो विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा सके। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ईमान की वास्तविकता ज़बान से इक़रार और दिल से उसकी पुष्टि है, उनकी राय दुरुस्त है और इस राय को पवित्र क़ुरआन और सुन्नत के ख़िलाफ़ क़रार नहीं दिया जा सकता। इसकी वजह यह है कि ईमान के दो मौलिक प्रकार हैं। एक प्रकार वह है जिसके मुक़ाबले में कुफ़्र का शब्द प्रयुक्त होता है। ईमान और कुफ़्र, ईमान की यह वह क़िस्म है जिसपर सांसारिक आदेशों का दारोमदार है। जो व्यक्ति इस प्रकार के ईमान का दावा करे और उसकी किसी कथनी और करनी से उसका खंडन न हो तो उसको सांसारिक मामलों की दृष्टि से मोमिन क़रार दिया जाएगा। शरीअत के ज़ाहिरी आदेश उसपर जारी होंगे, इस्लामी राज्य के नागरिक के रूप में उसको वे तमाम अधिकार और रिआयतें प्राप्त होंगी जो मुसलमानों को प्राप्त होती हैं।
ईमान का दूसरा अर्थ वह है जो निफ़ाक़ (मिथ्याचार) के मुक़ाबले में प्रयुक्त होता है। यह अर्थ वह है जिसपर आख़िरत के आदेशों का दारोमदार है, अगर ईमान वास्तविक है और दिल की गहराइयों से निकला है तो आख़िरत में नजात प्राप्त होगी, अल्लाह तआला वे दर्जे प्रदान करेगा जो ईमानवालों के लिए ख़ास हैं। यह वह क़िस्म है जिसमें कमी-बेशी भी होती है, जिसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा भी होता है, जिसकी शक्ति में कमी भी आ सकती है, इज़ाफ़ा भी होता है।
जहाँ तक ईमान के विभागों का सम्बन्ध है उनमें कुछ तो वे हैं जो इस्लाम के स्तम्भ हैं। चार स्तम्भ, इस्लाम ही के स्तम्भ हैं, कुछ शेष विभाग हैं जो दूसरे आदेश से इबारत हैं। उसी तरह से हार्दिक पुष्टि के लिए भी ईमान का शब्द प्रयुक्त होता है, बल्कि उर्दू और दूसरी भाषाओं में भी ईमान का शब्द दिल की पुष्टि और विश्वास के अर्थ में आम तौर से प्रयोग होता है। इस हार्दिक सन्तुष्टि और सुकून के लिए भी ईमान की शब्दावली प्रयुक्त होती है जो एक ईमानवाले को वास्तविक ईमान के बाद प्राप्त होता है। ईमान के इन चारों अर्थों को सामने रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ईमान की वास्तविकता और उसकी शर्तों के बारे में इस्लामी विद्वानों के दरमियान कोई वास्तविक मतभेद मौजूद नहीं है। और जो मतभेद बज़ाहिर इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) की बहसों में नज़र आता है, वह कोई वास्तविक मतभेद नहीं है। ईमानियात की समस्याओं पर चर्चा की जाए तो सबसे पहला मसला अल्लाह तआला के अस्तित्व, सृष्टि के रचयिता के अस्तित्व और मख़लूक़ात से उसके सम्बन्ध के प्रकार का मामला है। इस्लामी विद्वान जब सृष्टि के रचयिता के अस्तित्व के मसले से बहस करते हैं तो वे दुनिया के ‘हादिस’ होने के मामले पर भी बहस करते हैं। दुनिया के ‘हादिस’ होने का अर्थ यह है कि पूरी सृष्टि जो नज़र आ रही है अल्लाह तआला के अलावा जो कुछ भी दुनिया में मौजूद है या अतीत में मौजूद रहा है या आइन्दा मौजूद होगा, यह सब ‘हादिस’ है, यानी वह पहले मौजूद नहीं थीं, बाद में अस्तित्व में आया है। अल्लाह तआला का अस्तित्व ही वास्तव में प्राचीन है, बाक़ी जो कुछ है वह बाद में ज़ाहिर हुआ है।
इमामुल-हरमैन इमाम अब्दुल-मलिक अल-जुवैनी जो अपने ज़माने के पहली पंक्ति के मुतकल्लिमीन और पहली पंक्ति के फ़ुक़हा में से हैं, बल्कि फ़िक़्हे-शाफ़िई (रह॰) के द्वितीय संकलनकर्ताओं में गिने जाते हैं। इमाम शाफ़िई (रह॰) के बाद फ़िक़्हे-शाफ़िई के इतिहास में बहुत बड़ा दर्जा इमामुल-हरमैन का है। उन्होंने इन दोनों सिद्धान्तों पर ईमान लाना हर बुद्धि रखनेवाले वयस्क व्यक्ति का फ़र्ज़ क़रार दिया है। वे कहते हैं कि हर आक़िल बालिग़ (बुद्धि रखनेवाले वयस्क व्यक्ति) पर जो चीज़ सबसे पहले फ़र्ज़ होती है, वह यह कि सबसे पहले चिन्तन-मनन से, सृष्टि की गवाहियों और बौद्धिक तर्कों से अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान लाए, उसके बाद सृष्टि के ‘हादिस’ होने का यक़ीन उसको प्राप्त हो।
इस्लामी विद्वानों ने प्रायः और उलमाए-कलाम ने विशेष रूप से अल्लाह तआला के अस्तित्व के बौद्धिक तर्कों के मामले से बेहद दिलचस्पी ली है। अल्लाह के अस्तित्व के बौद्धिक तर्कों का मामला प्राचीनकाल से दार्शनिकों और धार्मिक चिन्तकों की दिलचस्पी का विषय रहा है। मुसलमान चिन्तकों से भी पहले बहुत-से दूसरे धर्मों के चिन्तकों ने, ईसाई मुतकल्लिमीन ने, यहूदी उलमाए-अक़ाइद ने और दूसरी क़ौमों के विद्वानों ने अल्लाह के अस्तित्व के बौद्धिक तर्कों से बहस की है। मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने आम तौर पर दो दलीलें बहुत अधिक बयान की हैं और इल्मे-कलाम की किताबों में बहुत मनोयोग से इन दोनों दलीलों पर बहस होती है। एक दलील, ‘दलीले-जौहरे-फ़र्द’ कहलाती है और दूसरी दलील, ‘दलीले-मुम्किनो-वाजिब’ के नाम से याद की जाती है। मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने इन दोनों तर्कों पर विस्तार से चर्चा की है और कोशिश की है कि उनके ज़माने में जो बौद्धिक तर्क प्रचलित थे, यूनानी तर्कशास्त्र एवं दर्शन के अनुसार जो शैली प्रचलित थी उससे काम लेकर अल्लाह के अस्तित्व को साबित किया जाए और यों इस्लामी अक़ीदे को तार्किक प्रमाणों से और अधिक ज़ेहन में बिठाया जाए।
लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लामा इक़बाल के शब्दों में ये तमाम प्वॉइंट्स एक मानसिक विलासिता का तो सामान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनसे विश्वास की कमज़ोरी का इलाज नहीं हो सकता। यह अजीब-ग़रीब प्वॉइंट्स या ये बौद्धिक बहसें इंसान के अन्दर विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सकतीं। पवित्र क़ुरआन से अन्दाज़ा होता है कि हर सद्बुद्धि रखनेवाले इंसान में एक स्वाभाविक भावना के रूप में यह बात मौजूद है कि वह सृष्टि के रचयिता पर ईमान रखता हो। सृष्टि के रचयिता पर ईमान चूँकि स्वाभाविक प्रवृत्ति में रख दिया गया है, इसलिए अच्छे स्वभाव पर अगर कोई पर्दा पड़ जाए तो इस पर्दे को उठाने की लिए मामूली-से प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। मामूली ध्यान से उन गवाहियों को इंसान के ज़ेहन में बिठाया जा सकता है जो इस पर्दे को उठाने में मदद दें। पवित्र क़ुरआन की यही शैली है। पवित्र क़ुरआन ने जिन तर्कों से काम लिया है वे निश्चय ही मज़बूत भी हैं, वे निस्सन्देह बौद्धिक तर्क भी हैं लेकिन उनका अन्दाज़ किसी कलात्मक और दार्शनिकतापूर्ण तर्कों का नहीं है, बल्कि उनका अन्दाज़ एक ऐसी तार्किकता का है जिसको एक आम आदमी भी समझ सके, इसमें ‘बुरहाने-ख़िताबी’ का प्रयोग भी है और ‘बुरहान’ और ‘दलील’ के शेष प्रकारों का प्रयोग भी है। लेकिन इन सबमें शब्द इस तरह के प्रयोग किए गए, अन्दाज़ और शैली ऐसी अपनाई गई है कि ग़ज़ाली (रह॰) और राज़ी (रह॰) के दर्जे के दार्शनिकों से लेकर आम इंसानों तक हर व्यक्ति अपनी सतह के अनुसार इन तर्कों को समझ सकता है।
‘मारिफ़ते-इलाही’ से क्या मुराद है? ‘मारिफ़ते-इलाही’ में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, इसको स्पष्ट भी मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने किया है। ‘मारिफ़ते-इलाही’ में सबसे पहले अल्लाह तआला की वहदानियत (एकत्व), फिर अल्लाह तआला के वे मौलिक गुण जो वहदानियत की अनिवार्य अपेक्षा हैं और जिन तक हर इंसान मामूली चिन्तन से पहुँच सकता है। उनपर ईमान भी अल्लाह पर ईमान की अनिवार्य अपेक्षा है। अल्लाह तआला का सर्वज्ञ होना, हर चीज़ का ज्ञान रखना, उसका क़ादिर (सामर्थ्यवान) होना, लाभ-हानि का मालिक होना, हर चीज़ का उसके अधिकार क्षेत्र में होना इत्यादि। ये वे गुण हैं जो अल्लाह पर ईमान की अनिवार्य अपेक्षा हैं। यह बात न केवल मुतकल्लिमीन और उलमाए-उसूल ने लिखी है, बल्कि इस्लामी दार्शनिकों ने भी यह बात बयान की है।
फ़ाराबी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘आराउ-अहलिल-मदीना-अल-फ़ाज़िलः’ में यह बात बयान की है कि अल्लाह के अस्तित्व पर ईमान में यह भी शामिल है कि उसके निजी नामों और गुणों पर ईमान रखा जाए, उसकी पूर्ण सामर्थ्य का पूर्ण आभास हो और अल्लाह के अस्तित्व की वास्तविकता और प्रकार का इतना ईमान हो जितना एक आम इंसान की समझ में आ सकता है। फ़ाराबी ने अपनी दार्शनिक शैली में अल्लाह के अस्तित्व के लिए मौजूद ‘अव़्वल’ की शब्दावली भी प्रयुक्त की है और ‘सबबे-अव्वल’ की शब्दावली भी प्रयोग की है। वह यह कहता है कि अल्लाह तआला का अस्तित्व तमाम मौजूद चीज़ों के लिए ‘सबबे-अव्वल’ की हैसियत रखता है। वह हर प्रकार के कमाल से विभूषित है और हर प्रकार की त्रुटि से मुक्त है। उस अस्तित्व के अलावा जो कुछ भी सृष्टि में मौजूद है वह किसी-न-किसी त्रुटि में मुब्तला है। जहाँ तक मौजूद ‘अव़्वल’ यानी अल्लाह तआला के अस्तित्व का सम्बन्ध है, उसका अस्तित्व दूसरे सब अस्तित्वों से श्रेष्ठ और प्राचीन है। इसलिए कि यह बात सम्भव नहीं है कि सृष्टि में कोई अस्तित्व ऐसा पाया जा सके जो अल्लाह के अस्तित्व से श्रेष्ठ और उसके अस्तित्व से प्राचीनतम हो। फ़ाराबी ने अल्लाह के अस्तित्व के बारे में जो कुछ कहा है और निस्सन्देह संक्षेप और व्यापकता के साथ कहा है। वह अपनी वास्तविकता और प्रकार की दृष्टि से उससे ज़्यादा विभिन्न नहीं है जो बाद में मुतकल्लिमीने-इस्लाम ने कहा। मुतकल्लिमीने-इस्लाम आम तौर पर यह बात कहते आए हैं कि अल्लाह के अस्तित्व को बयान करने में और उसके गुणों को विस्तृत रूप से बयान करने में वे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिएँ जो इंसान या अन्य भौतिक प्राणियों को बयान करने में प्रयुक्त होते हैं।
अब यह जौहर (सारतत्व), अर्ज़ (लम्बाई-चौड़ाई), माद्दा (पदार्थ), जिस्म (शरीर), जेहत (आयाम) आदि ये सब दार्शनिकतापूर्ण शब्दावलियाँ स्रष्ट चीज़ों को बयान करने में प्रयुक्त होती हैं। अल्लाह तआला समय और स्थान का भी रचयिता है, अल्लाह-तआला पदार्थ और आकृतियों का भी रचयिता है, अल्लाह तआला तमाम जौहर और विशालताओं का रचयिता है। इसलिए स्रष्ट वस्तुओं की शैली को प्रयोग करते हुए जब रचयिता को बयान किया जाएगा तो वह बयान हमेशा अधूरा और त्रुटिपूर्ण बयान होगा। इसलिए फ़ाराबी ने दूसरे मुतकल्लिमीने-इस्लाम की तरह यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि अल्लाह तआला को माद्दा और जौहर की शब्दावली में, या सूरत और शक्ल की शब्दावली में बयान नहीं करना चाहिए। इसलिए कि न अल्लाह तआला का अस्तित्व इस दृष्टि से माद्दा है, न उस दृष्टि से जौहर और अर्ज़ के दायरे में शामिल है, जो अन्य जीवों और भौतिकवाद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए कि उसका अस्तित्व, अस्तित्व के मामले में न केवल अत्यन्त उच्च और श्रेष्ठ स्थान रखता है, बल्कि उसका अस्तित्व अत्यन्त परिपूर्ण अस्तित्व है। वह अनादिकाल से है, सदैव रहनेवाला है, उसका अस्तित्व भी शाश्वत है, उसकी वास्तविकता भी शाश्वत है, न उसका कोई कारण है, न उसका कोई ‘अव्वल’ (आरम्भ) है, न उस का कोई ‘आख़िर’ (अन्त) है।
अबू-नस्र फ़ाराबी ने फ़रिश्तों को भी बयान करने की कोशिश की है और फ़रिश्तों को बयान करने में, या फ़रिश्तों की दार्शनिकतापूर्ण व्याख्या करने में उसने वे शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं जो दार्शनिकों के यहाँ उस ज़माने में प्रचलित थीं। ऐसा मालूम होता है कि शायद दार्शनिकों के यहाँ ‘अक़्ले-फ़अआल’ नाम से जो कहावत प्रसिद्ध थी, उसकी अबू-नस्र फ़ाराबी ने फ़रिश्तों से व्याख्या करने की कोशिश की है और यह बताया है कि जिन स्रष्ट जीवों को, या सृष्टि की जिन शक्तियों को इस्लामी शब्दावली में फ़रिश्तों के नाम से याद किया गया, ये वही शक्तियाँ हैं जिनके लिए यूनानियों ने और पश्चिमी दार्शनिकों ने ‘अक़्ले-फ़अआल’ या इस प्रकार की दूसरी शब्दावलियाँ प्रयोग की हैं।
अबू-नस्र फ़ाराबी और अन्य मुतकल्लिमीन की बहसों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि अल्लाह के अस्तित्व को बयान करने और उसके बारे में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि दर्शनशास्त्र और भौतिक शास्त्र की शब्दावलियों और कहावतों से परहेज़ किया जाए, उन शब्दावलियाँ से बचा जाए जो स्रष्ट वस्तुओं और भौतिकवाद को बयान करने में प्रयुक्त होती हैं। चुनाँचे ‘ऐन’ और ‘अर्ज़’, ‘मुरक्कब’ और ‘ग़ैर-मुरक्कब’, ‘ह्योला’ और ‘सूरत’। ये तमाम शब्दावलियाँ स्रष्ट वस्तुओं को बयान करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इन शब्दावलियों को सृष्टि के रचयिता के मामले में प्रयोग करना उचित नहीं। पवित्र क़ुरआन में इशारा कर दिया गया कि “कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह के जैसा क़रार दिया जा सके।” (क़ुरआन, 42:11) अल्लाह के जैसा का जैसा भी क़रार दिया जा सके। न उसका कोई प्रतिरूप है न उसका कोई उदाहरण है, न उसकी कोई उपमा है। वह अपने अस्तित्व में निराला और अपवाद है।
यही बात जो अबू-नस्र फ़ाराबी ने लिखी वही बात इमामुल-हरमैन ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘अल-इरशाद’ में जो इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) पर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किताब है, लिखी है। इमामुल-हरमैन ने इस बौद्धिक और दार्शनिकतापूर्ण तर्क शैली से जो उस ज़माने में प्रचलित थी और उस ज़माने की बौद्धिकता से ली गई थी, यह साबित किया है कि अल्लाह तआला का अस्तित्व जौहर, अर्ज़ और जिस्म आदि की विशिष्टताओं और आदेशों से परे और मुक्त है। इन सब विशिष्टताओं का अस्तित्व उस के यहाँ असम्भव है। हर वह चीज़ जो ‘हादिस’ हो यानी प्राचीन और आदिकालीन न हो और बाद में पैदा हुई हो वह अल्लाह तआला के निकट असम्भवों में से है। अत: घटनाओं और हादिसों और किसी ख़ास समय और स्थान से जुड़ाव ये सब बातें हवादिस में से हैं। उनको अल्लाह के अस्तित्व के लिए प्रयोग करना अल्लाह तआला के उच्च एवं श्रेष्ठ अस्तित्व के अनुकूल नहीं है।
इंसान के ईमानवाला होने की लिए केवल इतना मानना काफ़ी है कि अल्लाह तआला का अस्तित्व एकमात्र और निराला है, सृष्टि के कण-कण और चप्पे-चप्पे का ज्ञान रखता है, हर चीज़ पर सामर्थ्यवान है। अल्लाह तआला इन तमाम परिपूर्ण गुणों, सौन्दर्य गुणों, और प्रतापी गुणों से विभूषित है जो पवित्र क़ुरआन में और हदीसों में बयान हुई हैं। अल्लाह के ‘हय्य’ (हमेशा जिन्दा रहनेवाला) और ‘क़य्यूम’ (हमेशा क़ायम रहनेवाला) होने का और अलीम (सर्वज्ञ) होने की अनिवार्य अपेक्षा है कि यह समझा जाए कि वह समीअ (सब कुछ सुननेवाला) भी है और बसीर (अन्दर तक देख लेनेवाला) भी है। इमामुल-हरमैन ने ‘समअ’ (सुनने) और ‘बसर’ (देखने की क़ुव्वत) के साबित करने के लिए बौद्धिक तर्क भी बयान किए हैं, लेकिन यह बौद्धिक तर्क वे हैं जिनकी दरअस्ल कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तआला की तौहीद पर एक बार ईमान क़ायम हो जाए तो फिर शेष गुणों पर ख़ुद-ब-ख़ुद ईमान पैदा हो जाता है। इसलिए कि यह गुण अल्लाह के अस्तित्व की अनिवार्य अपेक्षा हैं।
इन तमाम पहलुओं में ईमान का मूल सिद्धान्त जिसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ‘अस्ल उसूल अल-बिर्र’ क़रार दिया है, यानी तमाम ख़ूबियों और नेकियों की अस्ल और बुनियाद, वह तौहीद का अक़ीदा है। इसलिए कि तौहीद के अक़ीदे पर ईमान होगा तो वे तमाम नैतिक और आध्यात्मिक खूबियाँ प्राप्त की जा सकेंगी जिनको इंसान प्राप्त करना चाहता है। शाह वलीउल्लाह ने तौहीद के चार बड़े दर्जे या मर्तबे बयान किए हैं। सबसे पहला मर्तबा तो यह है कि ज़ाते-वाजिबुल-वुजूद एक ही है और अस्तित्व का वह प्रकार जो अनिवार्य होने के दर्जे के लिए अनिवार्य है, वह सिर्फ़ अल्लाह तआला के अस्तित्व में निहित है। दूसरा दर्जा यह है, सृष्टि की जो बड़ी-बड़ी वस्तुएँ हैं, अर्शे-इलाहि, ज़मीन-आसमान और शेष वे सारी चीज़ें जो इंसान के अवलोकन में आ चुकी हैं या अवलोकन से बाहर हैं, उनका रचयिता और मालिक केवल और केवल अल्लाह तआला है। तीसरा दर्जा यह है कि तमाम सृष्टि का संचालन यानी प्राकृतिक संचालन जिसका उल्लेख किया जा चुका है, यह सिर्फ़ अल्लाह तआला के अधिकार में है। तौहीद का चौथा और आख़िरी दर्जा जो शाह वलीउल्लाह फ़रमाते हैं वह यह है कि इबादत का हक़दार अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है।
ये सारांश है इन बहसों का जो अल्लाह के अस्तित्व के बारे में इस्लामी दार्शनिकों और मुतकल्लिमाने-इस्लाम ने बयान की हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक और नैतिकता के शिक्षक इब्ने-मस्कवैह ने भी ‘अल-फ़ौज़ुल-अकबर’ में इन तर्कों की ओर संक्षिप्त-सा इशारा किया है।
तौहीद दरअस्ल मात्र एक अक़ीदा नहीं है, बल्कि अल्लामा इक़बाल के शब्दों में सृष्टि की सबसे बड़ी और सबसे महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली जीवित शक्ति है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि ‘नब्ज़े-मौजूदात में पैदा हरारत इससे है और मुस्लिम के तख़य्युल में हरारत इससे है’। यानी तौहीद ही तमाम स्रष्ट जीवों में हरारत और सरगर्मी का कारण है और इस्लाम के जितने विचार और सिद्धान्त हैं उन सबमें अगर शक्ति पैदा होती है तो तौहीद के अक़ीदे से पैदा होती है। तौहीद के अक़ीदे पर ईमान के लिए यह काफ़ी है कि इंसान तौहीद के इन चार दर्जों पर ईमान और यक़ीन रखता हो।
अल्लाह तआला की सृष्टि पर चिन्तन-मनन और विचार करने से यह यक़ीन और ईमान मज़बूत होता चला जाता है। इसी लिए पवित्र क़ुरआन में जगह-जगह सृष्टि पर चिन्तन-मनन की दावत दी गई है, रचयिता पर चिन्तन-मनन से मना किया गया है। इसलिए कि रचयिता के बारे में चिन्तन-मनन इंसान की क्षमता और वश से बाहर है। इंसान अगर इस रास्ते को अपनाए तो भटकने और ग़लती की सम्भावनाएँ अत्यन्त प्रबल और अधिक हैं। इसलिए हदीसों में इससे मना किया गया है। तौहीद पर ईमान की एक अनिवार्य अपेक्षा यह भी है कि इंसान शिर्क से बचकर रहे, शिर्क के रास्तों को पहचाने और उन तमाम विचारों और कर्मों से पूरी तरह बचकर रहे जिनमें शिर्क का लेशमात्र भी पाया जाता हो।
तौहीद पर ईमान के बाद इस्लाम का दूसरा बड़ा अक़ीदा पैग़म्बरी और रिसालत है। पवित्र क़ुरआन से पता चलता है कि पैग़म्बरी और रिसालत का सिलसिला इंसानियत की रचना के समय से ही शुरू हो गया था। अल्लाह तआला ने जब इंसानों को यह ज़िम्मेदारी देकर भेजा तो इस बात का प्रबन्ध किया कि इंसानों को अल्लाह तआला की ओर से मार्गदर्शन और निर्देश लगातार उपलब्ध होते रहें, चुनाँचे यह मार्गदर्शन लगातार उपलब्ध होता रहा और अल्लाह तआला की ओर से पैग़म्बर और रसूल भेजे जाते रहे। एक प्रसिद्ध हदीस में जो कि हज़रत अबू-ज़र ग़िफ़ारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने रिवायत की है और अनेक मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया है। इसमें कहा गया है कि पैग़म्बरों की कुल संख्या एक लाख चौबीस हज़ार (1,24000) है, जिनमें वे लोग जिनको रिसालत (ईशदूतत्व) के मंसब पर क़ायम किया गया, वे तीन सौ तेरह (313) की संख्या में थे।
इस्लामी विद्वानों ने पैग़म्बरी की वास्तविकता, उनका मर्तबा और पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। यह चर्चा टीकाकारों ने भी की है। वे पवित्र क़ुरआन की उन आयतों की व्याख्या में जहाँ पैग़म्बरी और पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) का ज़िक्र है, पैग़म्बरी के मक़ाम और मंसब को विस्तार से बयान करते हैं। इसी तरह से हदीसों के व्याख्याताओं ने और उलमाए-उसूल ने भी किसी हद तक पैग़म्बरी के मंसब पर चर्चा की है।
जहाँ तक पैग़म्बरी की मौलिक धारणा का सम्बन्ध है, यह धारणा बड़ी हद तक मुसलमानों, यहूदियों और एक हद तक ईसाइयों के कुछ वर्गों में समान है। यानी यह बात कि अल्लाह तआला की तरफ़ से इंसानों के मार्गदर्शन का प्रबन्ध हो, कुछ चुनिंदा और ख़ास इंसानों पर अल्लाह की तरफ़ से मार्गदर्शन अवतरित हो, वह मार्गदर्शन निश्चित और यक़ीनी हो और इंसानों के लिए उसका पालन अनिवार्य हो, यह धारणा इन तीनों क़ौमों और किसी हद तक कुछ दूसरी क़ौमों में मौजूद रही है। लेकिन यह एक अजीब बात है कि इन तीनों क़ौमों के दरमियान, बल्कि ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में इस्लाम और पश्चिम के दरमियान सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे विवादित समस्या पैग़म्बरी और रिसालते-मुहम्मदी की है। यह मात्र कोई धार्मिक या Theology का ईशू नहीं है, बल्कि दरअस्ल यह एक सांस्कृतिक समस्या है। यह मात्र सामयिक हितों का टकराव नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि वे यह समझते हैं कि अगर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर ईमान की समस्या को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे उनकी अधार्मिक व्यवस्था में बड़ी दराड़ें पड़ जाने का ख़तरा है। आधुनिक काल की पूरी अधार्मिक और सेक्युलर व्यवस्था नष्ट-विनष्ट हो जाती है, अगर रिसालते-मुहम्मदी पर ईमान को अनिवार्य स्वीकार कर लिया जाए और शरीअते-मुहम्मदी को अनुपालन योग्य व्यवस्था स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी से उनका मतभेद मात्र हितों का टकराव नहीं है, सलीबी जंगों में तो कोई हितों का टकराव नहीं था। सलीबी जंगों में वैश्विक सत्ता की कोई समस्या नहीं थी, सलीबी जंगों में अगर कोई मौलिक मतभेद था तो वह सिर्फ़ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी पर ईमान का मसला था। इसलिए यह मौलिक रूप से एक ऐसा मतभेद है जिसको हम पैराडायम का मतभेद कह सकते हैं।
पैराडायम का मतभेद ही दरअस्ल वह मूलभूत मतभेद है जो दो विभिन्न सभ्यताओं के दरमियान हो सकता है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी पर जो आपत्तियाँ पश्चिमवालों की तरफ़ से आज की जा रही हैं, ये कोई नई नहीं हैं। ये आपत्तियाँ क़ुरआन के अवतरण के अवसर पर मक्का के अधर्मियों की ओर से, अरब के इस्लाम विरोधियों की ओर से और उस ज़माने में मुसलमानों के समकालीन यहूदियों की ओर से भी की गई थीं। यह बात कि पवित्र क़ुरआन पुराने क़िस्से कहानियों का एक संग्रह है जो इधर-उधर से जमा करके बयान कर दिए गए हैं, यह बात पहले भी कही गई थी। यह बात कि क़ुरआन के संकलन में अमुक-अमुक का हाथ है और अमुक-अमुक स्रोतों से क़ुरआन की बातें ली गई हैं, यह बात भी पवित्र क़ुरआन में बयान हुई है। किसी निर्धारित पादरी का नाम लेकर कहना कि अमुक पादरी ने अमुक मौक़े पर ये बातें नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को सिखा दी थीं। यह बात भी उस ज़माने में कही गई। “अमुक इंसान इनको सिखाता है।” (क़ुरआन, 16:103) फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में (अल्लाह माफ़ करे) ऐसे आरोप और आपत्तियाँ जिनका प्रत्यक्ष रूप से हमला उनकी नीयत और संकल्पों पर हो, यह भी कोई नई बात नहीं है। ग़ज़वों के मुहर्रिकात, बनू-क़ुरैज़ा के साथ मामला, उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ज़ैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) के साथ निकाह का मामला, मक्का मुकर्रमा में विशुद्ध दीनी दावत और मदीना मुनव्वरा में राज्य के क़ियाम की बात और उसपर आपत्तियाँ। ये सब वे एतिराज़ात और सनदेह हैं जो पहले दिन से किए जा रहे हैं। प्राच्यविदों ने कोई नई बात दरयाफ़्त नहीं की है, जो नई बातें प्राच्यविद बयान करते हैं या नई आपत्तियाँ पेश करते हैं वे इतने कमज़ोर और बे-बुनियाद होते हैं कि जिनका जवाब देने की शायद ज़रूरत न हो, लेकिन फिर भी उनका जवाब सैंकड़ों, बल्कि हज़ारों बार दिया जा चुका है। प्राच्यविदों की ओर से उन बेसिर-पैर की बातों को लगातार दोहराया जाना इस बात की दलील है कि अपने दावे के विपरीत वह हक़ या तहक़ीक़ के परिणामों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
अब कुछ अर्से से कुछ प्राच्यविदों ने यह कहना शुरू किया है कि दरअस्ल अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दिल में अरबों के सुधार की भावना पैदा हुई और वे (अल्लाह की पनाह!) एक अरब क़ौमियत क़ायम करना चाहते थे। यह बात भी उतनी ही निराधार है जितनी निराधार शेष बातें हैं। दरअस्ल इस सारी भाग-दौड़ का कारण एक पर्दा है जो तास्सुब या किसी और कारण से इंसानों की बुद्धि पर पड़ जाता है। और एक बार वह पड़ जाए तो फिर बहुत-से स्पष्ट तथ्यों को देखना और समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है।
क्या पैग़म्बरी का कोई बौद्धिक प्रमाण दिया जा सकता है? क्या मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी को विशुद्ध बौद्धिक तर्कों से साबित किया जा सकता है? यह सवाल भी आरम्भ ही से मुतकल्लिमीने-इस्लाम के क्षेत्रों में चर्चा का विषय रहा है। दरअस्ल बौद्धिक प्रमाण की शब्दावली भी बहुत विवादित है और विभिन्न अर्थ रखती है। एक ईमानवाला, सद्बुद्धि रखनेवाला जब बौद्धिक प्रमाण की शब्दावली प्रयोग करता है तो उसका अर्थ और होता है, लेकिन जब एक अधर्मी भौतिकवादी बौद्धिक प्रमाण की शब्दावली प्रयोग करता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है। इस्लामी विद्वानों में से अनेक लोगों उदाहरणार्थ मौलाना रूम ने जगह-जगह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी के अक़ीदे को बौद्धिक और मानसिक ढंग से अपने पाठकों के ज़ेहन में बिठाने की कोशिश की है। इन लोगों ने पवित्र क़ुरआन की तर्क शैली को आगे बढ़ाते हुए मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पैग़म्बरी के सुबूत के लिए बुर्हानी, ख़िताबी, इस्तिदलाली हर प्रकार की शैलियों से काम लिया है।
अक़ीदे की यही तीन बड़ी-बड़ी बुनियादें हैं जिनपर अक़ीदों और ईमानियात की पूरी इमारत क़ायम है। इन्हीं बुनियादों और इनसे सम्बन्धित अन्य बातों की बौद्धिक और तार्किक व्याख्या ही इल्मे-कलाम (इस्लामी धारणाओं को बुद्धि द्वारा सिद्ध करने का ज्ञान) का मौलिक अभीष्ट है। आगे की चर्चा में इल्मे-कलाम का एक सरसरी परिचय और आम जायज़ा पेश किया गया है।
Recent posts
-

तज़किया और एहसान (शरीअत : लेक्चर# 8)
12 November 2025 -

तदबीरे-मुदन - राज्य और शासन के सम्बन्ध में शरीअत के निर्देश (शरीअत : लेक्चर# 7)
05 November 2025 -

इस्लाम में परिवार की संस्था और उसका महत्त्व (शरीअत : लेक्चर# 6)
24 October 2025 -
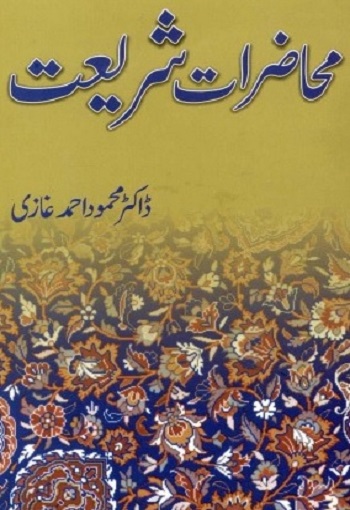
शरीअत का अभीष्ट व्यक्ति : इस्लामी शरीअत और व्यक्ति का सुधार एवं प्रशिक्षण (लेक्चर नम्बर-5)
15 October 2025 -
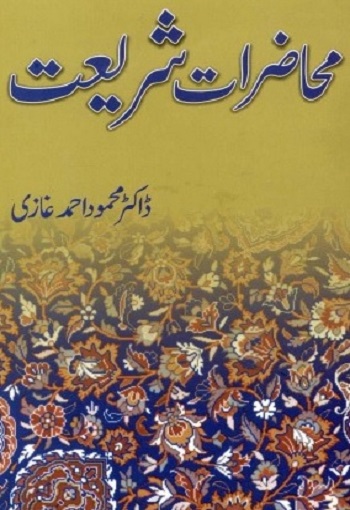
नैतिकता और नैतिक संस्कृति (शरीअत : लेक्चर # 4)
31 August 2025 -
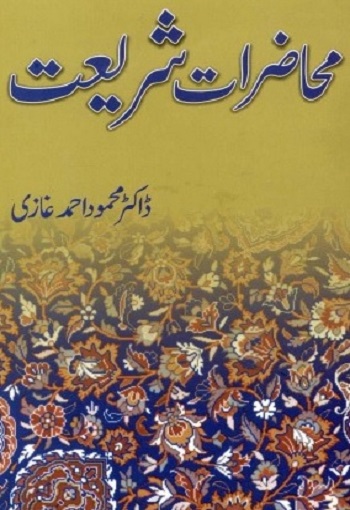
मुसलमान और मुस्लिम समाज (शरीअत : लेक्चर # 3)
28 August 2025