
अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में राज्य की भूमिका (लैक्चर-4)
-
अर्थशास्त्र
- at 23 December 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
आज की चर्चा का शीर्षक है अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में राज्य की भूमिका। यह बात पहले बताई जा चुकी है कि इस्लामी राज्य में अर्थव्यवस्था तथा व्यापार के मामले आम तौर से राज्य और सरकार के हस्तक्षेप से आज़ाद रहते हैं। राज्य को प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप के अधिकार कुछ विशेष और अपवाद स्वरूप प्राप्त हैं। आम तौर से इस्लाम की शिक्षा की प्रवृत्ति यह है कि बाज़ार, अर्थव्यवस्था और व्यापार की शक्तियाँ तथा उत्प्रेरक स्वयं ही स्वतंत्र और न्यायपरक ढंग से काम करते रहें तो राज्य को हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अलबत्ता राज्य का काम यह है कि वह व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करे। इस बात को निश्चित करे कि शरीअत के क़ानून और राज्य के आदेश पर अमल हो रहा है।
इस्लामी राज्य को इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग प्रभावकारी न होने पाएँ जो क़ानून और आदेश को नज़र-अंदाज़ करके अपने निजी हित के लिए बाज़ार की प्रवृत्तियों को ख़राब कर रहे हों। अपनी तरह राज्य आम लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध करेगा और व्यापारियों और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को क़ानून, पॉलिसी और प्रशासनिक सुविधाओं के द्वारा वह तमाम कारण उपलब्ध करेगा जो व्यापार और अर्थव्यवस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए कामों के लिए अपरिहार्य हैं।
हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधि की निगरानी, रैगुलेटरी फ़्रेमवर्क, पेशों का गठन और उन्हें नियमित करना, व्यक्तिगत स्वामित्व को शरीअत को सीमाओं के अंदर रखने के लिए कंट्रोल, मृत पड़े मामलों को पुनर्जीवित करने का उचित प्रबन्ध और फ़राइज़े-किफ़ाया (वे कर्तव्य जिन्हें कुछ मुसलमान भी निभा दें तो वे अदा हो जाएँ, परन्तु अगर कोई भी न निभाए तो सब गुनहगार हों) के मामले में ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, ये तमाम मामले राज्य की ज़िम्मेदारी में शामिल हैं। शरीअत के स्पष्ट आदेशों के अनुसार क़ीमतों का पहले से निर्धारण राज्य को नहीं करना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में राज्य को क़ीमतों के निर्धारण के द्वारा बाज़ार को कंट्रोल करने की पॉलिसी अपनानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर राज्य यह महसूस करे कि बाज़ार में कुछ तत्व अनावश्यक रूप से क़ीमतों में वृद्धि का ज़रिया बन रहे हैं, जमाख़ोरी की वजह से, ज़्यादा नफ़ाख़ोरी की वजह से या किसी और वजह से बाज़ार की क़ीमतों को ख़राब कर रहे हैं तो फिर राज्य को बतौर निगराँ (Caretaker) और रैगुलेटर के हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इन अपवाद परिस्थितियों में राज्य को ऐसे काम करने की इजाज़त है, जो क़ीमतों को उचित स्तर पर रखने में सहायता दें, ताकि तमाम सम्बन्धित वर्गों के अधिकार न्याय के साथ उपलब्ध किए जा सकें।
राज्य की ज़िम्मेदारीयों के सन्दर्भ में ‘फ़राइज़े-किफ़ाया’ का बहुत महत्व है। ‘फ़राइज़े-किफ़ाया’ से मुराद वे फ़राइज़ (कर्तव्य) हैं जो समष्टीय रूप से पूरे मुस्लिम समाज के ज़िम्मे हैं। अगर मुस्लिम समाज में से कुछ लोग इन कर्तव्यों को अच्छे तरीक़े से निभा रहे हों तो फिर आम मुसलमान इन ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस काम के लिए आगे न बढ़ें या कुछ लोग आगे बढ़ें, लेकिन वे प्रभावकारी और काफ़ी अंदाज़ में अपेक्षित स्तर के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा न कर पा रहे हों तो फिर पूरा मुस्लिम समाज इस कोताही का ज़िम्मेदार और इस कोताही की हद तक गुनहगार होगा।
मुस्लिम समाज के सदस्यों की संख्या ज़ाहिर है हर दौर में बहुत रही है और इसमें बढ़ोतरी होती रही है, इस वक़्त भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए मुस्लिम समाज को हमेशा इस बात की ज़रूरत है कि इसकी ओर से कोई संस्था या राज्य इन फ़राइज़ (कर्तव्यों) को पूरा करने का प्रबन्ध करे। राज्य के न होने या उसके द्वारा दिलचस्पी न लेने की स्थिति में समाज के नुमायाँ व्यक्तियों या नागरिक संगठनों को या जिनको आजकल सिविल सोसाइटी कहा जाता है, यह ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। इस तरह के संगठन इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रबन्ध करें। परन्तु यह ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा राज्य की है। राज्य को ऐसी संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिएँ जो मुस्लिम समाज को फ़राइज़े-किफ़ाया के करने में मदद दें और उन तमाम मामलों में जो ‘फ़राइज़े-किफ़ाया’ के प्रकार के हैं, एक सम्पर्ककर्ता का कर्तव्य निभाएँ। इन कर्तव्यों के अलावा आजकल आधुनिक काल में जिसको पूर्ण अर्थव्यवस्था या macro economics कहा जाता है, इसकी अपेक्षाओं की पूर्ति में राज्य की भूमिका मूल होती है। चूँकि आजकल का चलन यह है जिसका समर्थन अनुभव ने भी किया है, बुद्धि और तर्क ने भी किया है। और यह चीज़ शरीअत के आदेशों से टकराती नहीं है। इसलिए शरई तौर पर उसको अपनाना अच्छी बात है कि macro economics के मामलों में राज्य की भूमिका मुख्य हो। यह काम राज्य ही कर सकता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक भरपूर जायज़ा लेकर यह तय करे कि किन-किन विभागों में किस तरह के काम की ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा करने के लिए जिन उत्प्रेरकों का जायज़ा लेना चाहिए, जिन कारणों एवं कारकों को विकास देना चाहिए, जिन कारणों एवं कारकों को कंट्रोल करना चाहिए, यह काम राज्य ही कर सकती है। समाज में अगर बेरोज़गारी फैल रही है, जो आजकल की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बन गई है, तो बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए मुख्य भूमिका राज्य ही निभा सकता है। व्यक्ति या संस्थानों की भूमिका बेरोज़गारी के मामले में ज़ाहिर है कि बहुत सीमित होगी। फिर आजकल के दौर में वित्तीय और नक़दी पॉलिसी राज्य ही तय करता है। चूँकि आजकल सारा दारोमदार ज़रे-एतिबारी (विश्वसनीय मुद्रा अर्थात् सोने-चाँदी की मुहरें आदि) पर या काग़ज़ी सिक्के पर हो गया है और ज़रे-एतिबारी राज्य ही जारी कर सकता है। राज्य की ओर से इसका केन्द्र बैंक ही ज़रे-एतिबारी जारी करता है। इसलिए राज्य ही को यह तय करना पड़ता है कि इसकी मुद्रा नीति क्या होगी। वित्तीय मामलों के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या होगा। किस तरह और किस अंदाज़ से वह इस पॉलिसी को चलाएगा, कब और कितनी मुद्रा जारी करेगा, विदेशी मुद्रा के कितने भंडार अपने पास रखेगा। इन विदेशी मुद्रा के भंडारों में कितने होंगे जो देश के अन्दर रखे जाएँगे। कितने होंगे जो पूँजी निवेश की ग़रज़ से या दूसरे महत्वपूर्ण उद्धेश्य के लिए विदेश में रखे जाएँगे। यह काम व्यक्तियों के करने का नहीं है। यह काम केवल राज्य के करने का है और इसको राज्य ही करेगा।
इसके अलावा देश का सामान्य रूप से आर्थिक विकास राज्य का काम है। राज्य ही तय करेगा कि पूरे देश को विकास से लाभान्वित करने के लिए क्या-क्या कार्य किए जाने चाहिएँ। क्या-क्या प्राथमिकताएँ होनी चाहिएँ। यह फ़ैसला राज्य ही कर सकता है कि किन पहलुओं को ज़्यादा ध्यान का केन्द्र बनाया जाए और किन पहलुओं को फ़िल्हाल बाद के लिए छोड़ दिया जाए, तो कोई हरज नहीं है। विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देश में राज्य की यह भूमिका अत्यंत महत्व रखती है। हमारे देश में जहाँ कुछ इलाक़े अल्लाह की कृपा से ऐसे हैं जहाँ अल्लाह तआला ने हमें बहुत संसाधन प्रदान किए हैं। वहाँ हमारे बलूचिस्तान में कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित हैं। कुछ पूरे-पूरे ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई बैंक सिरे से नहीं पाया जाता। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें एक-आध केन्द्रीय सड़क के अलावा सड़कें नहीं हैं। संचार माध्यम न होने के बराबर हैं। सिंध के कुछ इलाक़ों में सैंकड़ों मील तक पानी नहीं पाया जाता। ये वे मामले हैं जो फ़िक़ही आदेशों के अनुसार ‘ज़रूरते-शदीदा’ (अत्यन्त आवश्यकता) का दर्जा रखते हैं।
इस्लामी शरीअत की माँग यह है कि सबसे पहले इन इलाक़ों पर भरपूर ध्यान लगाया जाए जो अत्यन्त मौलिक आवश्यकताओं से भी वंचित हैं। शरीअत के अनुसार राज्य के संसाधनों को कहीं और ख़र्च करना जायज़ नहीं है, हराम है, जब तक देश के कुछ लोग अपनी अत्यन्त मूल और शदीद ज़रूरतों से भी वंचित हैं। यह क्रम जिसका पहले भी कई बार उल्लेख किया जा चुका है, ‘ज़रूरियात’, ‘हाजियात’ और ‘तकमीलियात’ (या ‘कमालियात’) की शब्दावली के हवाले से इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बयान किया है, इस क्रम का आर्थिक विकास के प्रोग्राम में ध्यान रखना अनिवार्य है।
फिर पूर्ण अर्थव्यवस्था का एक और विभाग आयात एवं निर्यात में सन्तुलन भी है। आजकल यह मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य आयात-निर्यात में सन्तुलन पर निर्भर करता है। यह काम आम लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ राज्य को अपनी मूल भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर आयात तथा निर्यात का मामला केवल आम लोगों पर छोड़ दिया जाए तो फिर हर व्यापारी की कोशिश यही होगी कि ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, ज़्यादा-से-ज़्यादा उपभोग की वस्तुएँ आयात करे।
हर प्रकार की उपभोगी वस्तुएँ आयात करे, जिस चीज़ के भी ख़रीदार पाए जाते हों, वह जहाँ से भी मिले देश के अन्दर आयात कर ले। ज़ाहिर है इसका परिणाम यह निकलेगा कि हर चीज़ के लिए देश के बाज़ार खुल जाएँगे। स्थानीय उद्योग और इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। आयात एवं निर्यात में सन्तुलन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए राज्य ही को यह तय करना चाहिए कि किन चीज़ों का आयात देश के हित में है, किन चीज़ों का निर्यात देश के हित में है। और किन चीज़ों का आयात एवं निर्यात देश के लिए हानिकारक है।
जिन चीज़ों का आयात एवं निर्यात देश के लिए लाभप्रद है उनके आयात एवं निर्यात के लिए राज्य संसाधन उपलब्ध करेगा। सुविधाएँ पैदा करेगा। प्रोत्साहन के जितने उचित और ज़रूरी कार्य हो सकते हैं वह राज्य करेगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आयात एवं निर्यात देश के लिए हानिकारक है। आम लोगों के लिए कष्ट का कारण है तो राज्य उसपर प्रतिबन्ध लगाएगा। उदाहरणार्थ देश के अंदर खाद्यान्नों की कमी हो और किसी पड़ोसी देश में भी सख़्त कमी हो तो इस स्थिति में खाद्यान्नों के आयात की अगर खुली छुट्टी दे दी जाए और यह काम व्यक्तियों के अधिकार में हो तो तमाम बड़े-बड़े व्यापारी और जमाख़ोर खाद्यान्न दूसरे देश को निर्यात कर देंगे। विदेशी मुद्रा कमाएँगे और देश के अन्दर आम लोगों को ज़रूरत के अनाज से वंचित होना पड़ेगा।
इस तरह के बहुत-से मामले हो सकते हैं। जहाँ आजकल के हालात और ज़रूरतों को देखते हुए राज्य को आयात एवं निर्यात के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है और यह हस्तक्षेप अपरिहार्य है। जो चीज़ अपरिहार्य हो तो उसके लिए कारण अपनाना भी अपरिहार्य होता है। शरीअत का सिद्धान्त मैं पहले भी बता चुका हूँ। “जिस चीज़ पर किसी वाजिब का दारोमदार हो वह भी वाजिब (अनिवार्य) हो जाती है।” प्रसिद्ध हकीमुल-इस्लाम और नामवर शाफ़िई फ़क़ीह अल्लामा इज़ुद्दीन-बिन-अब्दुस्सलाम ने कहा है कि “जो चीज़ उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम हो वह उच्चतम माध्यम समझी जाएगी, जो चीज़ निकृष्टतम उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम हो वह निकृष्टतम माध्यम समझी जाएगी।” यों ज़रिये और माध्यम के आदेश वही होंगे जो उस उद्देश्य के हैं जिनके लिए वह माध्यम अपनाया गया है।
पूर्ण अर्थशास्त्र यानी macro economics के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्धेश्य होते हैं। ये वे लक्ष्य और उद्धेश्य हैं जो राज्य को पूरे करने चाहिएँ और राज्य की ज़िम्मेदारी है कि अपनी पॉलिसी, क़ानून और निगरानी के अधिकार के द्वारा इन उद्धेश्यों को प्राप्त करे। देश में आर्थिक विकास, सन्तुलन और समरूपता के साथ हो तो पूरा देश विकास करेगा, वर्ना कुछ इलाक़े पीछे रह जाएँगे। ऐसा हो तो यह शरीअत के अनुसार न्याय के ख़िलाफ़ है। राज्य की यह ज़िम्मेदारी है कि न्याय और समता के इस्लामी लक्ष्य को प्राप्त करे। हर सम्भव राज्य का प्रयास यह होना चाहिए कि देश के विभिन्न क्षेत्रों और आम लोगों के विभिन्न वर्गों के दरमियान आर्थिक विकास की दर में बहुत अधिक अन्तर न हो। थोड़ा-बहुत अन्तर तो अपरिहार्य होता है जिससे बचा नहीं जा सकता। बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र होंगे। बड़े-बड़े बैंकों के कार्यालय बड़े शहरों में होंगे। बड़ी-बड़ी व्यापारिक कंपनियाँ बड़े शहरों में होंगी। ये चीज़ें छोटी बस्तियों में या गाँवों में नहीं हो सकतीं। उनके आर्थिक प्रभाव और आर्थिक परिणाम बड़े शहरों तक सीमित रहेंगे। इस हद तक तो अन्तर होना अपरिहार्य है, लेकिन जैसा अन्तर हमारे देश में पाया जाता है और काफ़ी समय से मौजूद है, जिसको दूर करने का किसी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक कोई परिणामदायक प्रयास नहीं किया। यह शरई तौर पर अत्यन्त अप्रिय है।
पूर्ण अर्थव्यवस्था के दूसरे लक्ष्य में क़ीमतों में स्थिरता का मामला भी शामिल है। क़ीमतों में स्थिरता राज्य के आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। अगर क़ीमतों में स्थिरता न हो तो न आयात सही हो सकता है न निर्यात दुरुस्त हो सकता है। क़ीमतों में स्थिरता न हो तो वेतनभोगी वर्ग और सीमित आय रखनेवाले लोग अपनी ज़िंदगी के मामलों को दुरुस्त नहीं कर सकते। क़ीमतों में स्थिरता इसलिए भी ज़रूरी है कि मुद्रा स्फीति जो आजकल ज़रे-एतिबारी (विश्वसनीय मुद्रा अर्थात् सोना-चाँदी आदि) का एक अनिवार्य परिणाम हो गई है उसे कम-से-कम रखा जाए। जब तक ज़रे-एतिबारी की व्यवस्था दुनिया में मौजूद है उस वक़्त तक पूर्ण रूप से मुद्रा स्फीति को समाप्त करना शायद सम्भव नहीं है। अलबत्ता उचित कार्रवाइयों और उपायों से उसे कम-से-कम रखा जा सकता है। इतना कम-से-कम जो आम लोगों की क्षमता से बाहर न हो। इस काम के लिए ज़रूरी है कि एक सन्तुलित वित्तीय और मुद्रा नीति बनाई जाए जिसपर राज्य की तमाम संस्थाएँ काम करें। वित्तीय और मुद्रा नीति बनाना राज्य का ही काम है और यह राज्य के आर्थिक लक्ष्यों में से एक है।
सरकारी ख़र्चों को कम-से-कम करना और देश में बेरोज़गारी को ख़त्म करना भी पूर्ण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण उद्धेश्यों में शामिल है। राज्य के ख़र्चे कम-से-कम हों, यह बात हमेशा से अर्थशास्त्रियों और विचारकों की चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रही है। इस्लामी विचारकों ने भी इसपर चर्चा की है। शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, अल्लामा इब्ने-ख़लदून ने और अनेक इस्लामी विद्वानों ने इस बात के महत्व पर रौशनी डाली है कि राज्य के ख़र्चों को कम-से-कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए। शाह वलियुल्लाह ने एक जगह पेशों की विस्तार से चर्चा की है और कुछ पेशों को बेकार और फ़ुज़ूल पेशे क़रार दिया है और कहा है कि इन पेशों के करनेवाले अगर समाज में बढ़ जाएँ, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो यह राज्य के ख़ज़ाने पर अनावश्यक रूप से बोझ होता है और इसका परिणाम पूरे समाज की तबाही और बर्बादी के रूप में निकलता है। चुनाँचे अगर कला एवं साहित्य के नाम पर शेअरो-अदब के नाम पर किसी और तफ़रीह के नाम पर हज़ारों, लाखों इंसान सरकारी खज़ाने पर बोझ बन जाएँ तो सरकारी ख़ज़ाना आख़िरकार इस नुक़्सान को बर्दाश्त करने के क़ाबिल नहीं रहता।
पाकिस्तानियों के लिए पीआईए (Pakistan International Airlines) की मिसाल बहुत नुमायाँ और शिक्षाप्रद है। पीआईए जो पाकिस्तान के लिए अत्यन्त गर्व के योग्य संस्था थी, जो एक ज़माने में पूरी दुनिया के लिए नमूना था, जिसने दुनिया की वे बड़ी-बड़ी एयरलाइनें बनाईं, जो आज दुनिया में बड़ी-बड़ी एयर लाइनें समझी जाती हैं। जिनका आरम्भ पीआईए के हाथों हुआ, वही पीआईए आज तबाही और बर्बादी का शिकार है और उसके सुधार की तमाम कोशिशें पिछले तीस वर्षों में असफल हो गई हैं। इसकी बड़ी वजह, शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि पीआईए के ख़ज़ाने पर ऐसी-ऐसी गतिविधियों का बोझ लाद दिया गया जो अनुत्पादन गतिविधियाँ थीं। किसी राजनैतिक लीडर ने यह चाहा कि इसके समर्थकों को पीआईए में नौकरियाँ दे दी जाएँ, किसी के दिल में यह आया कि जितने नाचने-गानेवाले ग्रुप हैं उनको पीआईए के ख़र्च पर पाला जाए, किसी के दिल में यह आया कि जितने लोग इस संस्था से जुड़े हैं उनको ज़िंदगी-भर मुफ़्त सफ़र की सुविधाएँ दे दी जाएँ। इन सब नाजायज़ कामों का परिणाम यह निकला कि ख़र्चे तो बढ़ते चले गए, लेकिन आय कम होती चली गई और अब वह स्थिति पूरी तरह सामने आ गई है जिससे बचने की ख़ातिर इस्लामी विचारकों ने, शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी और दूसरे लोगों ने यह ताकीद की थी कि सरकारी संसाधनों को सीमित ढंग से ख़र्च किया जाए और जहाँ-जहाँ सरकारी संसाधन ख़र्च किए जाते हैं उन रास्तों को कम-से-कम रखा जाए।
यह तो बात थी पूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में राज्य की ज़िम्मेदारी की जहाँ राज्य ही की अस्ल ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी micro economics का सम्बन्ध है वहाँ भी राज्य की ज़िम्मेदारी बिलकुल ही ख़त्म नहीं हो जाती। वहाँ राज्य की भूमिका मूल रूप से केवल निगरानी की और रहनुमाई की है, एक अच्छे मध्यस्थ की है, संरक्षण तथा प्रोत्साहन की है और सुविधा उपलब्ध करनेवाले की है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या आंशिक अर्थशास्त्र में कुछ मामले ऐसे आ जाते हैं जिनसे राज्य की संस्थाएँ ही बेहतर और प्रभावकारी तरीक़े से निबट सकती हैं। उदाहरणार्थ उपभोक्ता और उद्योगपति के रवैये का गहन विश्लेषण, उपभोक्ता क्या चाहता है, उद्योगपति क्या चाहता है और इन दोनों के हितों को परस्पर अनुकूल किस तरह किया जाए। जहाँ ये दोनों हित अनुकूल हो जाएँगे और क़ुदरती और स्वाभाविक दृष्टि से अनुकूल होंगे वहाँ समाज के लिए बेहतरी होगी। इन दोनों को अगर बनावटी रूप से अनुकूल किया जाए, अनावश्यक रूप से उपभोक्ता के रवैये को बदला जाएगा, अनावश्यक रूप से उद्योगपति के हित को तर्जीह दी जाएगी तो इससे आर्थिक व्यवस्था में विघ्न पड़ेगा।
आपूर्ति और माँग का मामला भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण मामला है। आम हालात में राज्य इसमें दख़ल नहीं देगा। अगर आपूर्ति और माँग की क़ुव्वतें स्वाभाविक रूप से काम करती रहें, अगर नैतिकता और शरीअत की सीमाओं का पालन किया जाए तो उसके नतीजे में कोई समस्याएँ पैदा नहीं होतीं। लेकिन जहाँ नैतिकता, शरीअत या क़ानून का दामन हाथ से छोड़ दिया जाए वहाँ आपूर्ति और माँग की क़ुव्वतों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौक़ा नहीं मिलता, ऐसे में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। क़ीमतों में और जो अभीष्ट आपूर्ति है या जो वास्तविक सप्लाई है इन दोनों में तार्किक और उचित सम्पर्क होना चाहिए। यह काम राज्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति स्वयं ही यह काम करते रहें, व्यापारी और ख़रीदार, पैदावार करनेवाले उद्योगपति, खेती पेशा लोग ये सब वर्ग मिल-जुलकर ख़ुद ही सन्तुलन और न्याय के साथ यह काम करते रहें तो फिर राज्य को हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ना राज्य को यह काम करना पड़ेगा और एक ऐसे सन्तुलित नुक़्ते तक पहुँचने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी जो अपरिहार्य है।
इस्लामी अर्थशास्त्र के बारे में यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि इसका आधार न्याय, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण, धन-संकेन्द्रण की मनाही और हतोत्साहन, जमाख़ोरी के निषिद्ध होने, व्यक्तिगत स्वामित्व के सम्मान और उत्पादन के साधन तक पहुँचने में समानता जैसी महत्वपूर्ण धारणाओं और सिद्धान्तों पर है। इन्हीं बुनियादों पर इस्लामी अर्थशास्त्र की इमारत खड़ी होती है। ये तमाम वे मामले हैं जो आजकल राज्य की ओर से क़ानून बनाने की भी अपेक्षा करते हैं और पॉलिसी बनाने की अपेक्षा भी करते हैं, और जब तक राज्य प्रभावकारी निगरानी के द्वारा इन क़ानून और पॉलिसियों पर अमल न कराए तो न न्याय की माँगें पूरी हो सकती है, न न्यायपूर्ण वितरण के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, न धन-संकेन्द्रण को रोका जा सकता है, न जमाख़ोरी को समाप्त किया जा सकता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्लामी अर्थव्यवस्था एक दृष्टि से कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था है। यह पश्चिमी अर्थों में कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि यह इस्लामी अर्थों में कंट्रोल्ड है कि राज्य अपने कंट्रोल के द्वारा शरीअत के आदेशों के लागू करने को निश्चित बनाए। शरीअत के आदेशों का पालन कराए। शरीअत ने जिन चीज़ों को निषिद्ध ठहराया हो, उनसे रोके और उन्हें करनेवालों को उचित सज़ा दे। ‘रिबा’ (ब्याज) के हराम (निषेध) पर आजकल के दौर में जब तक राज्य का हस्तक्षेप और पूरी मदद न हो कार्यान्वयन नहीं हो सकता। ‘ग़रर’ (धोखा) और ‘क़िमार’ (जूआ) शरीअत में हराम है। ग़रर और क़िमार की आजकल इतने रूप प्रचलित हो गए हैं कि जब तक राज्य क़ानून के द्वारा उनका निषेध न करे और नीति के द्वारा लगातार उनको हतोत्साहित न करे उस समय तक इन निषिद्ध चीज़ों से बचना मुश्किल है।
न्याय इस्लामी व्यवस्था का मूल स्तम्भ है। शरीअत के तमाम आदेशों का दारोमदार न्याय पर है। पवित्र क़ुरआन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तमाम आसमानी शरीअतों का तमाम पैग़म्बरों का, और तमाम आसमानी किताबों का मूल लक्ष्य यह था कि लोग न्याय पर क़ायम हो जाएँ। न्याय का सबसे महत्वपूर्ण और मूल प्रकार जिससे हर इंसान को वास्ता पड़ता है वह सामूहिक न्याय है। क़ानूनी न्याय यानी अदालती न्याय कि आपका मुक़द्दमा है, आप अदालत में चले गए वहाँ से न्याय के अनुसार फ़ैसला हो गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका तमाम इंसानों से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। सौ में एक-आध का मुक़द्दमा अदालत में होता है, बाक़ी अठानवे-निनानवे प्रतिशत लोगों का अदालतों से सीधा सम्पर्क नहीं होता। लेकिन सामूहिक न्याय का सम्बन्ध सबसे होता है। हर इंसान को पैदावार के संसाधनों और आय के संसाधनों की ज़रूरत है। आय के संसाधनों का वितरण अगर न्याय के अनुसार न हो, समाज में सामाजिक न्याय मौजूद न हो, तो फिर हर इंसान ज़ुल्म का शिकार हो जाता है।
न्याय का विलोम अन्याय है। इसी लिए इस्लामी विद्वानों ने लिखा है कि हर ख़ैर (भलाई) न्याय है और हर शर (बुराई) ज़ुल्म (अन्याय) है। न्याय रौशनी है और अन्याय अँधेरा है। हदीस में आया है, सहीह बुख़ारी में है “ज़ुल्म क़ियामत के दिन सख़्त अँधेरों की शक्ल में सामने आएगा।” यह इसलिए है कि न्याय तौहीद (एकेश्वरवाद) का अनिवार्य परिणाम है। अगर तौहीद पर वास्तविक ईमान हो तो न्याय का सिद्धान्त अपनाया जाना अपरिहार्य है। इब्ने-ख़लदून ने लिखा है कि न्याय के बिना विकास सम्भव नहीं है, ज़ुल्म से विकास रुक जाता है। विकास रुकने से राज्य बर्बाद हो जाते हैं। न्याय का वास्तविक कार्यान्वयन शरीअत के लागू होने से ही हो सकता है। शरीअत के लागू हुए बिना वास्तविक न्याय सम्भव नहीं है। जहाँ वास्तविक न्याय सम्भव नहीं है वहाँ वास्तविक और सन्तुलित विकास भी सम्भव नहीं है। वास्तविक विकास जहाँ नहीं होगा वहाँ अन्याय होगा। अन्याय से रहा-सहा विकास भी रुक जाएगा और विकास रुकने से राज्य तबाह हो जाते हैं। यह बात इब्ने-ख़लदून ने भी लिखी है और दूसरे बहुत-से इस्लामी इतिहासकारों और विचारकों ने भी लिखी है।
न्याय की प्राप्ति के मूल कारक शरीअत के मूल स्रोतों में बयान हुए हैं। ये वही कारक हैं जिनको आजकल कल्याणकारी समाज की आवाज़ कहा जाता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और मूल कारक यह है कि धन-वितरण की व्यवस्था न्यायपूर्ण हो। धन-संकेन्द्रण को शरीअत इसी लिए नापसंद करती है कि धन-संकेन्द्रण की उपस्थिति में सामूहिक न्याय सम्भव नहीं है। शरीअत के आदेश धन-वितरण की व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने के लिए हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आय के संसाधनों को न्यायसंगत रूप से जुटाने को निश्चित बनाया जाए। जब तक समाज के हर व्यक्ति को उसकी प्रतिभाओं के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार और समाज के प्रचलित आर्थिक स्तर के अनुसार रोज़ी के संसाधन उपलब्ध न किए जाएँ, धन-वितरण की न्यायसंगत व्यवस्था क़ायम नहीं हो सकती। आय के संसाधन उपलब्ध करने से तात्पर्य यह नहीं है कि हर व्यक्ति को घर बैठे सरकारी पेंशन मिले। शरीअत मुफ़्तख़ोरों के वर्ग पैदा नहीं करना चाहती। शरीअत यह चाहती है कि हर वह व्यक्ति जो अपनी रोज़ी कमा सकता है, जिसको अल्लाह ने शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या किसी और तरह की प्रतिभा दी है, वह इस प्रतिभा को इस्तेमाल करके जायज़ रोज़ी कमा सके। जायज़ रोज़ी कमाने के लिए जब एक व्यक्ति घर से निकले तो उसके रास्ते में कोई बनावटी रुकावट न हो। एकाधिकार न हों, जमाख़ोरियाँ न हों, अनावश्यक रूप से ज़ुल्म की दीवारें खड़ी न की गई हों।
रोज़गार की सुविधा उपलब्ध हो, रोज़गार की सुविधा उपलब्ध करना राज्य की ज़िम्मेदारी भी है, व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी भी है और विशेष रूप से उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जिनको अल्लाह तआला ने ज़्यादा संसाधन प्रदान किए हैं। जिनके पास दौलत ज़्यादा है, उद्योग हैं, ज़मीनें हैं, बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाएँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी यह है कि वे रोज़गार की सुविधाओं को ज़्यादा-से-ज़्यादा सार्वजनिक करें। राज्य अपनी पॉलिसी के द्वारा इस काम को आसान बनाएगा, क़ानून के द्वारा आसान बनाएगा। क़ानून के द्वारा उन रास्तों को बंद करेगा जो रोज़गार की सुविधा के रास्ते में रुकावट का कारण बनते हों।
उनमें से एक महत्वपूर्ण बात संसाधनों का पूरा इस्तेमाल भी है। जिसको आजकल optimum ultilization कहते हैं। वह शरीअत का भी मंशा है। शरीअत का आदेश यह है कि अल्लाह ने जो रोज़ी दी है, जो साधन प्रदान किया है उसकी पूरी स्वीकारोक्ति और इस एहसान को पूरी तरह मानना चाहिए। इसकी एक मात्र शक्ल यह है कि उसका इस्तेमाल पूरी तरह हो। जो-जो फल और लाभ अल्लाह ने उसमें रखे हैं इंसान उन सबको प्राप्त करे। छोटे-से-छोटे से माध्यम से लेकर बड़े-से-बड़े माध्यम तक का पूरा और बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। किसी चीज़ को फ़ुज़ूल क़रार देकर बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की दी हुई हर चीज़ का बेहतर-से-बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए यह ज़रूरी है कि इस बात का ज्ञान और महारत प्राप्त की जाए कि किसी चीज़ का बेहतर-से-बेहतर इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा घरेलू जानवर जो मर जाए, जिसको लोग उसके घर से बाहर फेंक देते हैं, उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि उसको किसी ऐसी तरह इस्तेमाल करो कि इसके लाभकारी अंग बिलकुल बर्बाद न हों। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में देखा कि मुर्दा बकरी पड़ी हुई है, जो किसी ने फेंक दी थी, उन्होंने फ़रमाया कि “बकरी मुर्दा है इसको फेंक दिया, लेकिन इसकी खाल को इस्तेमाल किया जा सकता था। दबाग़त (Tanning) के द्वारा उसकी खाल का चमड़ा बनाया जा सकता था। यह चमड़ा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जहाँ चमड़ा इस्तेमाल होता है।” इससे स्पष्ट रूप से यह निर्देश मिलता है कि किसी चीज़ को भी बिना पूरी तरह इस्तेमाल किए नष्ट करना सही नहीं है। यह है संसाधनों का पूर्ण उपयोग।
फिर संसाधनों का उचित उपयोग भी ज़रूरी है और उचित वितरण भी ज़रूरी है। जब तक संसाधनों का उचित वितरण नहीं होगा, संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होगा। मैं पहले ज़मीन का उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को इतनी ज़मीन दे दी जाए कि उसको वह ख़ुद आबाद न कर सके, अपने संसाधनों से उसको आबाद न करा सके तो यह संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि उन संसाधनों के वितरण पर पुनर्विचार किया जाए और जिस व्यक्ति के पास अनावश्यक संसाधन हैं या अतिरिक्त संसाधन हैं वे उससे लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाएँ जिसके पास संसाधन नहीं हैं।
राज्य की ज़िम्मेदारियों में सार्वजनिक वित्त का मामला हर दौर में अनिवार्य समझा गया, उसको हमेशा एक महत्वपूर्ण समस्या समझा गया कि राज्य के आम वित्तीय प्रबन्धन को कैसे संगठित किया जाए। राज्य की आय की मदें क्या-क्या हों और उनको कहाँ-कहाँ ख़र्च किया जाए। यही वजह है कि सार्वजनिक वित्त राज्य की आर्थिक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल समस्या है। इस्लाम के प्रमुख दौर में सार्वजनिक वित्त के जो संसाधन थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण ज़कात थी जो ढाई प्रतिशत के हिसाब से वुसूल की जाती थी। ‘उश्र’ और ‘उशूर’ दोनों दस-दस प्रतिशत के हिसाब से वुसूल किए जाते थे। ‘उश्र’ कृषि पैदावार पर मुसलमान अदा करते थे और ‘उशूर’ व्यापारिक सामान की आयात पर वुसूल किया जाता था। यह व्यापारिक टैक्स भी दस प्रतिशत होते थे। जो व्यापारी बाहर से सामान लेकर हमारे देश में आएगा वह दस प्रतिशत अदा करेगा। जो व्यापारी यहाँ से सामान बाहर लेकर जाएगा वह दूसरे देश को दस प्रतिशत अदा करेगा।
ये कस्टम ड्यूटी हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने लगाई थी और बाद में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने विस्तार से इसके आदेश संकलित किए जिसके आधार पर कस्टम ड्यूटी को जायज़ समझा गया। इस्लामी राज्य बाहर से आनेवाले व्यापार के सामान पर उचित कस्टम ड्यूटी लागू कर सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने दस प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लागू की थी, इसलिए कि उनके दौर में दूसरे राज्य मुसलमान व्यापारियों से दस प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लिया करते थे। आज की परिस्थितियों के हिसाब से कस्टम ड्यूटी कम-ज़्यादा हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, देश के आर्थिक हितों, देश की पैदावार और ज़रूरतों को सामने रखकर राज्य कस्टम ड्यूटी में कमी-बेशी कर सकता है। इस कस्टम ड्यूटी का उल्लंघन इसी तरह शरई रूप से नाजायज़ है, जिस तरह शेष आदेशों का उल्लंघन शरीअत की दृष्टि में नाजायज़ है।
खनिज उत्पादनों पर ‘ख़ुमुस’ यानी बीस प्रतिशत हुआ करता था। ‘फ़ै’ सौ प्रतिशत राज्य की मिल्कियत हुआ करता था। ‘फ़ै’ से मुराद वह आय होती थी जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य को उसके प्रभाव की वजह से प्राप्त हो। जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य के स्वामित्व में आए, जिसका आम लोगों के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध न हो। ग़ैर-मुस्लिमों से ‘ख़िराज’ (टैक्स) और ‘जिज़या’ लिया जाता था जो ‘ज़कात’ और ‘उश्र’ का विकल्प था। ग़ैर-मुस्लिम ज़कात अदा नहीं करते थे, वह ज़कात की बजाय ‘जिज़या’ दिया करते थे। ग़ैर-मुस्लिम ‘उश्र’ नहीं दिया करते थे, वे ‘उश्र’ की जगह ‘ख़िराज’ अदा किया करते थे। ख़िराज और जिज़या दोनों का निर्धारण राज्य की अपनी समझ से होता था। राज्य अपनी समझ के अनुसार ख़िराज और जिज़ये का निर्धारण करता था। इस निर्धारण में मूल आदेश यह था कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, मुश्किल पैदा न की जाए। अदा करनेवाले की क्षमता और हैसियत के अनुसार उससे जिज़या और ख़िराज लिया जाए, उसकी क्षमता से बाहर और वश से बढ़कर उसपर बोझ न डाला जाए। इस विषय की हदीसें भी आई हैं। इस विषय को विस्तार से फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने संकलित भी किया है।
राज्य की ज़िम्मेदारियों में सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी जो शुरू से अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुबारक दौर से जारी रही, वह इस्लाम के लिए लड़नेवालों के वेतन और अतिये (तोहफ़े) हुआ करते थे। इस्लाम के आरम्भिक काल में बाक़ायदा वेतनभोगी फ़ौज की धारणा नहीं थी। तमाम वयस्क मुसलमान पुरुष योद्धाओं की ज़िम्मेदारियाँ आवश्यकता के अनुसार पूरी करते थे और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उनको तलब किया जा सकता था। इस काम के लिए वे अपने व्यापार, अपने कारोबार, अपनी ज़मीनें सब छोड़-छाड़कर जिहाद (इस्लाम की ख़ातिर लड़ने) के लिए निकल जाया करते थे। उस ज़माने का यह जिहाद कोई दो-चार दिन का मामला नहीं होता था। सरहद पर जाने में कई-कई महीने लग जाते थे। जंग कई-कई महीने चलती थी। वापसी में कई-कई महीने लगते थे। कभी-कभी इस पूरी प्रक्रिया में एक-एक साल, बल्कि दो-दो वर्ष तीन-तीन वर्ष लग जाया करते थे। इस दौरान मुजाहिदीन (इस्लाम के लिए लड़नेवालों) के घरवाले, मुजाहिदीन की आर्थिक ज़रूरतें, जिनमें व्यवहारत: तमाम मुसलमान शामिल थे, उनकी देख-भाल राज्य के ज़िम्मे होती थी। इसलिए राज्य ने मुजाहिदीन के वेतन तय किए जो आम तौर से उन संसाधनों से अदा किए जाते थे जो विजयों के परिणामस्वरूप प्राप्त होते थे।
हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में जब तमाम मुजाहिदीन के बाक़ायदा वेतन तय किए गए तो हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सबके वेतन बराबर रखे। उनका अपना वेतन और एक आम मुजाहिद सहाबी या ताबिई के वेतन के बराबर था। वह यह फ़रमाते थे कि कमी-बेशी और अज्र में ज़्यादती यह अल्लाह तआला के यहाँ जाकर होगी। सांसारिक मामलों की हद तक हम सबको बराबर रखेंगे और सबको वेतन बराबर देंगे। इसलिए कि आर्थिक ज़रूरतें सबकी एक जैसी हैं। घरवाले सबके साथ हैं। खाना-पीना, रोज़ी, इलाज, शिक्षा, यह सबको प्राप्त करनी है। इसलिए वेतनों में कमी-बेशी की धारणा उनके ख़याल में उचित नहीं थी।
जब हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का ज़माना आया तो उन्होंने अपने इजतिहाद से काम लिया। वह इजतिहाद जिसपर आज तक कार्यान्वयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेवाओं की दृष्टि से लोग बराबर नहीं हैं, इसलिए वे वेतन में भी बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम के लिए ज़िंदगियाँ क़ुर्बान करने में लोग बराबर नहीं रहे, तो वेतन में बराबर कैसे हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के धर्म को फैलाने में लोगों की कोशिशें बराबर नहीं हैं तो सुविधाओं और भत्तों में भी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने मुजाहिदीन की विभिन्न श्रेणियाँ तय कीं। आजकल के लिहाज़ से हम कह सकते हैँ कि इन्होंने वेतनों के ग्रेड तय किए। सबसे बड़ा ग्रेड या सबसे बड़ा वेतन जिसके लिए ‘अतिया’ का सम्मानित शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जो तय किया गया वह अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ख़ानदानवालों का तय किया गया। जिन लोगों का सम्बन्ध बनी-हाशिम और बनी-मुत्तलिब से था, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पड़दादा और उनके भाई मुत्तलिब की औलाद से था, वे नुबूवत के ख़ानदान में शुमार किए गए। उसके लिए कि इन दोनों भाइयों की औलाद और उनके दूसरे सम्बन्धी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के अत्यन्त जोशीले और निष्ठावान समर्थकों में से थे और उनकी औलाद ने हर दौर में, हर ज़माने में, हर मुश्किल में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का भरपूर साथ दिया। जब शेबे-अबी-तालिब में तमाम मुसलमान क़ैद हुए तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ख़ानदान के यही दो बड़े ग्रुप थे जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ शेबे-अबी-तालिब में क़ैद रहे। इसलिए सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनका दर्जा रखा। उनके बाद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की पाक बीवियों (अज़वाजे-मुतह्हरात) का। उनके बाद बद्र की जंग में हिस्सा लनेवालों का, फिर उन मुहाजिरीन का जो बद्र की जंग में शरीक नहीं हो सके, लेकिन बाद के ग़ज़वात (जंगों) में शरीक रहे। फिर उन अंसार का जो बद्र में भी शरीक रहे। फिर उन अंसार का जो बद्र में शरीक नहीं हो सके, लेकिन बाद के ग़ज़वों (जंगों) में शरीक रहे। इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने इस्लाम में सीनियारिटी और सेवाओं के दृष्टि से वेतनों के स्तर तय किए।
ये मापदंड चलते रहे और हर ज़माने के लोग उनका पालन करते रहे। यह बात सम्भवत: बहुत-से पाठकों के लिए दिलचपसी की होगी कि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का वेतन जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार मक़रीज़ी ने लिखा है छः हज़ार दिरहम वार्षिक तय हुआ था। और यह बात मैं बता चुका हूँ कि हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने सबके वेतन बराबर कर दिए थे, इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं, इसका कोई विवरण तो किसी किताब में नहीं मिला, लेकिन हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि तमाम मुसलमान सिपाहियों के, लोगों के और विधवाओं के वेतन या अतिये उसके बराबर होंगे। छः हज़ार दिरहम सालाना के हिसाब से अगर वेतन उनका हो तो पाँच सौ दिरहम मासिक के बराबर बनता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि उस ज़माने में चाँदी का निसाब दो सौ दिरहम था। दो सौ दिरहम आजकल के लिहाज़ से हमारे यहाँ के साढ़े बावन तोला चाँदी के बराबर होते थे। गोया दो सौ दिरहम साढ़े बावन तोला चाँदी के मूल्य के बराबर होते थे। इस दृष्टि से पाँच सौ दिरहम का अंदाज़ा लगाया जाए तो वह एक सौ बीस तोला चाँदी के लगभग बने। जो क़ीमत आज बाज़ार में एक सौ बीस तोला चाँदी की है, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वह मासिक वेतन मुसलमान सिपाहियों का रहा होगा। सम्भव है यहाँ किसी के ज़ेहन में यह ख़याल पैदा हो कि हमने तो जो घटनाएँ सुनी हैं वे इससे विभिन्न मालूम होती हैं। उदाहरणार्थ सुना है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर (रज़ियल्लाहु अन्हु) की पत्नी मीठा पकाना चाहती थीं, उसके लिए घर में सामान नहीं था। इन्होंने मासिक वेतन में से बचाकर इतनी रक़म बचाई कि मीठा बना सकें। यह बात भी दुरुस्त है। अस्ल में सिद्दीक़ अकबर (रज़ियल्लाहु अन्हु) अपना वह वेतन वुसूल नहीं करते थे जो सहाबा ने उनके लिए निर्धारित किया था। जितनी रक़म उनकी कम-से-कम ज़रूरतों के लिए अपरिहार्य होती थी, उतनी रखकर बाक़ी बैतुलमाल में वापस कर दिया करते थे। यही हाल हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का भी रहा। इसलिए ये लोग जो अपने-आपपर असाधारण सख़्ती करते थे उसका उत्प्रेरक उनकी निजी सादगी-पसंद जीवन-शैली और व्यक्तिगत परहेज़गारी और निस्पृहता थी। उन लोगों को हर वक़्त यही ख़याल रहता था कि अगर हमने अपने-आपपर कोई रक़म ऐसी ख़र्च कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो यह आइन्दा आनेवालों के लिए क़ानून और सुन्नत का दर्जा ले लेगी। इसलिए कि ख़ुलफ़ाए-राशिदीन की सुन्नत (तरीक़ा) भी शरीअत के मूलस्रोतों में एक महत्वपूर्ण दर्जा रखता था। इसलिए ये लोग विशेष रूप से अपने ऊपर वह सख़्ती किया करते थे जो बादवालों ने नहीं की और न उनको ज़रूरत महसूस हुई।
अब आज का एक ज़ाहिर-परस्त या ऊपरी सतह देखनेवाला समीक्षक जब देखता है कि बाद के किसी शासक ने अपने रहन-सहन में वह सादगी या सख़्ती नहीं अपनाई जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनाई थी या हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनाई थी तो वह इसको इस्लाम से विमुख होना समझता है। हालाँकि यह इस्लाम से विमुख होना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा वेतन वुसूल करे और इसके अनुसार काम भी करता हो तो वह शरई तौर से न केवल जायज़ है बल्कि पसंदीदा है। यह बात कि कोई व्यक्ति अपने जायज़ और स्वीकृत वेतन का अधिकतर हिस्सा वापस कर दे, तो यह मात्र उसका निजी और व्यक्तिगत फ़ैसला है, यह दरअस्ल तक़्वा और ज़िम्मेदारी का वह उच्चतम स्तर है जिसपर अगर कोई व्यक्ति आसीन होना चाहे, स्वयं ही उसको अपनाना चाहे तो अपना सकता है। किसी से यह माँग करना या किसी से यह आशा रखना कि हर व्यक्ति ऐसा ही रवैया अवश्य अपनाएगा यह शरीअत का आदेश नहीं है।
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने ज़माने में अगरचे वेतनों की व्यवस्था बराबर नहीं रखी थी और प्रतिष्ठित सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की सेवाओं और इस्लाम में उनके पहले और बाद में आने की वजह से उनके अतियों में कमी-बेशी की थी। लेकिन कहा जाता है कि अपनी मुबारक ज़िन्दगी के आख़िरी दिनों में वह यह समझते थे कि सुविधाओं और अतियों में यह कमी-बेशी उचित नहीं है और सही रवैया वही है जो हज़रत अबू-बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपनाया था। एक-आध बार उन्होंने यह बात कही थी कि इसी रवैये या इसी पॉलिसी को दोबारा अपनाना चाहिए। एक मर्तबा फ़रमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगले वर्ष सबसे कम सिपाहियों के वेतन, सबसे ऊँचे दर्जे के सिपाही के बराबर कर दूँगा। और एक आम सिपाही का वेतन भी दो हज़ार दिरहम कर दूँगा और ख़ुदा की क़सम! जब तक बैतुलमाल की रक़म में बढ़ोतरी होती रहेगी मैं वेतनों में बढ़ोतरी करता रहूँगा। जितना माल आएगा उतना ही गिन-गिनकर लोगों को देता जाऊँगा। और अगर माल इतना आया कि मैं उसको गिनकर न दे सका तो मैं बर्तनों में भर-भरकर दे दूँगा। और वह भी सम्भव न हुआ तो बोरीयाँ भर-भरकर दूँगा। इसलिए कि यह आम लोगों ही के संसाधन हैं। आम लोगों तक पहुँचने चाहिएँ।
इससे यह अंदाज़ा ज़रूर होता है कि कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) यह चाहते थे कि आम लोगों की ज़रूरतों में कोई कमी न की जाए और राज्य के पास अगर संसाधनों हों तो उनको भरपूर अंदाज़ से इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हर व्यक्ति तक उसके प्रभाव पहुँचें। एक और मौक़े पर उन्होंने फ़रमाया कि अगर मैं अगले वर्ष ज़िंदा रहा तो मैं एक सिपाही का वेतन चार हज़ार दिरहम कर दूँगा। एक हज़ार दिरहम इस काम के लिए कि वह अपने हथियारों पर ख़र्च करे, बेहतर-से-बेहतर हथियार प्राप्त करे। एक हज़ार दिरहम उसके निजी ख़र्चों के लिए, एक हज़ार दिरहम उसके घरवालों के ख़र्चों के लिए और एक हज़ार दिरहम उसके घोड़ों की तैयारी के लिए। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सिपाहियों के ये वेतन उनकी निजी ज़रूरतों के लिए भी थे और उन तमाम संसाधनों और हथियारों के लिए भी थे जिनका अधिकतर भाग आज राज्य ख़ुद बर्दाश्त करता है। आज का सिपाही अपना हथियार ख़ुद उपलब्ध नहीं करता। अपनी सवारियाँ ख़ुद उपलब्ध नहीं करता। अपनी जीप और टैंक ख़ुद लेकर नहीं आता। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि देश के सुरक्षा बजट का अगर एक बटा चार हिस्सा सिपाहियों के वेतनों, सुविधाओं, तैयारी और अन्य रिआयतों पर और तीन बटा चार हिस्सा दूसरे संसाधन और हथियारों पर ख़र्च हो तो यह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) की इस पॉलिसी के ऐन अनुसार होगा। यह सम्भवत: हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के आख़िरी ज़माने की बात है जब वह ‘अतिये’ की इस व्यवस्था पर नए सिरे-से विचार कर रहे थे। उबैदा सलमानी जो प्रसिद्ध ताबिई हैं और इस रिवायत के उल्लेखकर्ता हैं, उनकी मुलाक़ात हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उनके आख़िरी दिनों में ही हो सकती थी। इससे पहले हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) से उनकी मुलाक़ात की सम्भावना कम है, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इस इच्छा की पूर्ति का अवसर नहीं मिला कि वह कम-से-कम लोगों के वेतन उच्च-से-उच्च लोगों के बराबर कर देते। “मैं सबसे निचले वर्ग के सिपाहियों के वेतन सबसे ऊँचे वर्ग के सिपाहियों के बराबर कर दूँगा ताकि वह अता (प्रदान करने) में बराबर हो जाएँ।” लेकिन फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बाद जब हज़रत उसमान ग़नी (रज़ियल्लाहु अन्हु) ख़लीफ़ा हुए तो इन्होंने भी इसी पॉलिसी को बरक़रार रखा, जिसके अनुसार सिपाहियों के वेतनों में फ़र्क़ पाया जाता था।
हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) के बारे में दोनों तरह की रिवायतें मिलती हैं। उनका ज़माना ख़ासी अफ़रातफ़री और हंगामी हालात में गुज़रा। इसलिए निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल है कि उनके दौर में सिपाहियों के वेतन बराबर हो गए थे या कमो-बेश थे। एक रिवायत जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वह यह है कि उन्होंने सबके वेतन बराबर कर दिए थे। कुछ लोगों का ख़याल है कि नहीं, बल्कि उनके ज़माने में भी वही पॉलिसी जारी रही जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से चली आ रही थी। बहरहाल हज़रत अली (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अगर वेतन बराबर भी किए थे तो उनके बाद फिर उस पॉलिसी पर क़ायम नहीं रहा जा सका और वेतनों में कमी-बेशी ही का रवैया जारी रहा और आज तक जारी है।
जिन चीज़ों को ‘अतायात’ (‘अतिया’ का बहुवचन) कहा जाता था उनमें मुजाहिदीन का वेतन तो ख़ैर होता ही था, मुजाहिदीन के पीछे छूटनेवाले रिश्तेदारों को भी पेंशन मिलती थी। मुजाहिदीन के अलावा राज्य के जितने कारकुन थे उनके वेतन भी बैतुलमाल से होते थे। अपंगों की पेंशनें भी बैतुलमाल के ख़र्चे में शामिल थीं। वे लोग जो ख़ुद रोज़ी न कमा सकें, वे मुसलमान हों या ग़ैर-मुस्लिम, उनको पेंशन राज्य से मिलती थी। सोशल सिक्योरिटी अलाउंस जिसको हम कह सकते हैं वह भी मिलता था।
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने से भी पहले से ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के ज़माने से इस्लामी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विभाग ‘हिस्बा’ हुआ करता था। ‘हिस्बा’ यों तो एक अलग संस्था थी जो अर्ध-न्यायिक अधिकार रखती थी। और आम तौर से सामाजिक न्याय, सामाजिक नैतिकता और इस्लामी राज्य के सामूहिक लक्ष्य की सुरक्षा का कर्तव्य पूरा करती थी। लेकिन इन ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ उसके कर्तव्यों में बाज़ार की देख-भाल भी शामिल थी। व्यापारियों की निगरानी भी शामिल थी और यह बात कि बाज़ार में कोई किसी के साथ ज़ुलमो-ज़्यादती न करे, मिलावट न करे, धोखाधड़ी न करे। इस प्रकार के कामों की निगरानी भी ‘हिस्बा’ की संस्था किया करती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि ‘हिस्बा’ की व्यवस्था का इस्लामी अर्थव्यवस्था से गहरा सम्बन्ध था। बाज़ार के ‘मुहतसिब’ (लोकपाल) अलग-अलग हुआ करते थे। कृषि पैदावार के ‘मुहतसिब’ अलग होते थे। आम कमज़ोर इंसानों के साथ, बल्कि जानवरों के साथ न्याय भी ‘हिस्बा’ के फ़राइज़ में शामिल था। यह बात कि जानवरों के इस्तेमाल में उनके साथ ज़ुल्म न किया जाए, ज़्यादती न की जाए, किसी जानवर पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ न डाला जाए। यह निगरानी ‘हिस्बा’ की व्यवस्था किया करती थी।
आज भी राज्य की आर्थिक पॉलिसियों को निश्चित बनाने के लिए जो संस्थाएँ क़ायम हैं या आगे क़ायम की जाएँ उनको वे अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं जो ‘हिस्बा’ की संस्थाओं को दी जाती थीं। एक दृष्टि से वे संस्थाएँ जो सरकार की आर्थिक पॉलिसियों की निगरानी का कर्तव्य निभा रही हैं, उनपर कार्यान्वयन को निश्चित बना रही हैं वे ‘हिस्बा’ ही की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। ‘हिस्बा’ की एक ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक भी निभा रहा है जो बैंकों का ‘मुहतसिब’ है। ‘हिस्बा’ की ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी (Corporate Law Authority) जिसको कहा जाता था वह भी निभा रही है। यह व्यापारिक वर्गों की ‘मुहतसिब’ है। मिलावट को चेक करने की संस्थाएँ हैं। नाप-तौल के पैमाने को निश्चित करने की संस्थाएँ हैं। ये सब वे संस्थाएँ हैं जो इस्लामी दौर में ‘हिस्बा’ कहलाती थीं। आज ये संस्थाएँ अलग-अलग हो गई हैं। उनको अलग-अलग भी रखा जा सकता है, एक भी रखा जा सकता है और किसी एक बड़ी संस्था का अंग भी बनाया जा सकता है।
इस्लामी राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य ‘एहयाउल-मवात’ भी था, यानी मुर्दा ज़मीनों की आबादकारी (स्थानांतरगमन)। मुर्दा ज़मीनों की आबादकारी के बारे में कई हदीसें मौजूद हैं जो सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और हदीस की बहुत-सी किताबों में मौजूद हैं। ये हदीसें विभिन्न शब्दों में उल्लिखित हुई हैं। “जिसने किसी मुर्दा ज़मीन को आबाद किया वह उसकी है।” “जिसने किसी ऐसी ज़मीन को आबाद किया जो किसी की न थी वह उसका ज़्यादा हक़दार है।” इन हदीसों की रौशनी में इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने जो आदेश संकलित किए हैं, जिनको क्रमानुसार करने में ख़ुलफ़ाए-राशिदीन (चार आदर्श ख़लीफ़ा) की कार्य-नीति को सामने रखा गया है। उनके अनुसार ‘एहयाउल-मवात’ के लिए राज्य की इजाज़त इमाम अब्बू-हनीफ़ा (रह॰) के नज़दीक अपरिहार्य है। फुक़हा की ख़ासी संख्या इस राय से सहमति व्यक्त करती है कि सरकार की इजाज़त से कोई भी ग़ैर-ममलूका ज़मीन (वह ज़मीन जिसका कोई मालिक न हो) आबादकारी के लिए कोई भी शहरी प्राप्त कर सकता है। और यह ज़मीन बिना किसी पारिश्रमिक और बिना किसी क़ीमत के अलाट की जाएगी। अगर तीन वर्ष के दौरान वह शहरी इस ज़मीन को आबाद करने में सफल हो गया तो वह ज़मीन उसकी मिल्कियत क़रार पा जाएगी और अगर वह तीन वर्ष में ज़मीन को आबाद करने में सफल न हो सका तो राज्य को अधिकार है कि या तो और अधिक मोहलत दे दे या ज़मीन उससे वापस ले-ले।
प्रसिद्ध सहाबी हज़रत बिलाल-बिन-हारिस अल-मज़नी, (ये हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन नहीं हैं, यह दूसरे बिलाल हैं) इनको अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मदीना मुनव्वरा के क़रीब अक़ीक़ के इलाक़े में एक बहुत बड़ी ज़मीन दे दी थी। सहाबा ने बाद में कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! इस ज़मीन में फ़ुलाँ प्रकार की पैदावार होती है, जो आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर वह एक व्यक्ति के पास रही तो शायद उसके प्रभाव सही न हों। इसपर वह ज़मीन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनसे वापस ले ली और दूसरी एक ज़मीन उनको दी जिसकी आबादकारी का उन्होंने वादा किया, लेकिन वह उसको आबाद नहीं कर पाए। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अपने ज़माने में जब यह देखा कि हज़रत बिलाल-बिन-हारिस इस ज़मीन को आबाद नहीं कर पाए तो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उनसे वह ज़मीन वापस ले ली और दूसरे मुसलमानों को अलाट कर दी।
ज़मीनों की अलाटमेंट का विस्तृत विवरण हदीसों में कसरत से मिलता है। विशेष रूप से सरकारी और ग़ैर-आबाद ज़मीनों के विभिन्न लोगों को अलाटमेंट का विवरण हदीस, शरहों (व्याख्याओं) हदीस और फ़िक़्ह की किताबों में विस्तार के साथ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और तीन ख़लीफ़ाओं के ज़माने की बहुत-सी मिसालें इमाम अबू-यूसुफ़, इमाम अबदुर्रज़्ज़ाक़, यह्या-बिन-आदम और इमाम अबू-उबैद ने कसरत से नक़्ल की हैं। हदीस की लगभग सभी किताबों में कहीं-न-कहीं ये घटनाएँ बयान हुई हैं। इन सबसे निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीअत का लक्ष्य यह है कि कोई सरकारी ज़मीन बेकार न रहे और कोई ग़ैर-आबाद ज़मीन बेकार न पड़ी रहे। यह उसी सिद्धान्त पर कार्यान्वयन की एक शक्ल है जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि संसाधनों का अधूरा इस्तेमाल न किया जाए और तमाम उपलब्ध संसाधनों का बेहतर-से-बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इसलिए कि संसाधनों का इस्तेमाल जितना बढ़ेगा समाज की ख़ुशहाली और राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी तो समाज के सबसे पिछड़े वर्गों की ज़रूरतें पूरी होंगी। ‘कफ़ाफ़’ का दर्जा हर एक को प्राप्त हो जाएगा।
आर्थिक ज़रूरतों में ‘कफ़ाफ़’ सबसे पहला दर्जा है, जिससे मुराद वे कम-से-कम अनिवार्य और अपरिहार्य अपेक्षाएँ हैं जो हर इंसान को फ़ौरी तौर से दरकार हैं। ‘कफ़ाफ़’ के बाद दूसरा दर्जा ज़रूरतों का है। वह ज़रूरतें जो अनिवार्य और स्थायी प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। वे स्थायी भी हैं और अनिवार्य भी हैं। लिबास की ज़रूरत इंसान को स्थायी रूप से है। यह नहीं कि आज आपने लिबास उपलब्ध कर दिया तो पूरी ज़िंदगी ज़रूरत न पड़े। यह ज़रूरत हमेशा रहेगी और अनिवार्य है। कोई ज़माना ऐसा नहीं आ सकता कि इंसान को लिबास की ज़रूरत न हो। उनके बाद ‘हाजियात’ का दर्जा होता है। ‘हाजियात’ वे हैं जो अनिवार्य तो हैं, लेकिन ज़रूरतों से कम हैं। ये ज़रूरतों के मुक़ाबले में कम दर्जे की हैं। उमूमन स्थायी होती हैं, लेकिन कभी-कभी अस्थायी भी हो सकती हैं। उनके बाद ‘तकमीलियात’ का दर्जा आता है। जिनकी हैसियत हमेशा अतिरिक्त की होती है। ये असीमित हैं, इनकी कोई सीमा-रेखा नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हालात बेहतर-से-बेहतर हों। शरीअत की प्रवृत्ति और स्वभाव यह है कि ‘कफ़ाफ़’ और ज़रूरतों के लिए तो राज्य के संसाधन पूर्ण रूप से ख़र्च किए जाएँ। ‘हाजियात’ के लिए राज्य के संसाधन वहाँ ख़र्च किए जाएँ-जहाँ उपलब्ध हों और जितने उपलब्ध हों उतने ही ख़र्च किए जाएँ। ‘तकमीलियात’ का जहाँ तक सम्बन्ध है, वे चूँकि असीमित हैं इसलिए अगर उनपर कंट्रोल न किया जाए, उनको सीमाओं के अनुसार न बनाया जाए तो यह प्रवृत्ति अप्रिय रंग ले सकती है। एक हदीस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “अगर आदम के किसी बेटे के पास दो घाटियाँ सोने से भरी हुई हों तो वह तीसरी घाटी की तलाश में निकल पड़ेगा।” यह इंसान का स्वभाव है। ख़ुद पवित्र क़ूरआन का कथन है “और निश्चय ही वह (इंसान) धन के मोह में बड़ा दृढ़ है।” (क़ुरआन, 100:8) और “कंजूसी और माल की मुहब्बत इंसान के दिल में बिठा दी गई है।” इसलिए इस रवैये को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस भावना को सीमाओं में रखने के लिए ही शरीअत ने ग़नी (निस्पृह) बनने की शिक्षा भी दी है। क़नाअत (सन्तोष) और ज़ुहद (संयम) की शिक्षा दी है। यह शिक्षा इसी लिए है कि ‘तकमीलियात’ का यह दर्जा सीमाओं से बाहर न जाने पाए। इस दर्जे को सीमाओं के अंदर पूरा करने की ज़िम्मेदारी व्यक्तियों की है। व्यक्ति अगर ‘तकमीलियात’ प्राप्त करना चाहें तो करें। राज्य के संसाधनों में अगर गुंजाइश हो, कफ़ाफ़, ‘ज़रूरियात’ (ज़रूरतों) और ‘हाजियात’ के तक़ाज़े पूरे करने के बाद भी अगर संसाधन बच रहें तो फिर राज्य के संसाधन ‘तकमीलियात’ में भी ख़र्च किए जा सकते हैं। राज्य की अस्ल और मूल ज़िम्मेदारी ‘कफ़ाफ़’ की है। ‘कफ़ाफ़’ में मूल और अपरिहार्य रूप से तीन चीज़ें तो अवश्य ही और हर हाल में शामिल हैं। भूखे को खाना खिलाना, बे-लिबास को लिबास उपलब्ध करना, बे-घर को घर उपलब्ध करना। रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्धता ‘कफ़ाफ़’ है और यह पूरे मुस्लिम समाज के ज़िम्मे ‘फ़र्ज़े-किफ़ाया’ की तरह अनिवार्य है। इस अनिवार्य कार्य को या ‘फ़र्ज़े-किफ़ाया’ को आम लोगों की ओर से राज्य निभाएगा, इसलिए कि राज्य आम लोगों का वकील है। आम लोग मुवक्किल हैं, राज्य उनका वकील है। इसलिए मुवक्किल की ओर से वकील इस फ़र्ज़ को पूरा करेगा। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) में से कुछ लोगों ने यह लिखा है, जिनमें अल्लामा इब्ने-हज़म का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया है, कि अगर राज्य अपने इन तक़ाज़ों को पूरा न करे या राज्य इन कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता और ढीलापन दिखाए और समाज में ऐसे लोग मौजूद हों जिनको रोज़ी पेट भरकर न मिलती हो, ऐसे लोग मौजूद हों जिनके पास तन ढाँपने को लिबास न हो, सिर छुपाने को छत न हो तो वे ज़बरदस्ती ख़ुद संसाधनयुक्त लोगों से अपना हक़ वुसूल कर सकते हैं।
इस्लामी राज्य में कभी इस तरह की नौबत नहीं आई, लेकिन इस मिसाल से यह ज़ाहिर करना मक़सद है कि दर्जा ‘कफ़ाफ़’ की उपलब्धता को इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने आम लोगों के ज़िम्मे ‘फ़र्ज़े-किफ़ाया’ क़रार दिया है। अगर समाज के संसाधनयुक्त लोग अपनी आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहें, ‘इन्फ़ाक़’ (अल्लाह की राह में ख़र्च करने) के आदेश पर अमल करते रहें, अनिवार्य ‘सदक़ात’ अदा होते रहें तो निश्चित रूप से आशा की जा सकती है कि ‘कफ़ाफ़’ का दर्जा हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ‘कफ़ाफ़’ की इस धारणा को कुछ इस्लामी विद्वानों ने ‘किफ़ालते-आम्मा’ के शब्द से भी याद किया है। यहाँ यह बात याद रखना ज़रूरी है कि ‘किफ़ालते-आम्मा’ का यह हक़ ज़कात के अलावा है। पवित्र क़ुरआन में एक जगह आया है “और उन (दौलतमंदों) के मालों में माँगनेवाले और वंचित का भी हक़ है।” (क़ुरआन, 51:19) एक जगह पवित्र क़ुरआन में स्पष्ट रूप से सूरा-2 (बक़रा) की आयत-177 “तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक......” में ज़कात के अलावा भी माली ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। चुनाँचे एक हदीस भी है जिसमें कहा गया है कि “ज़कात के अलावा भी माल में समाज और राज्य का हक़ है।” अल्लामा आलूसी ने भी यही लिखा है। दूसरे अनेक क़ुरआन के विचारकों ने लिखा है कि ‘किफ़ालते-आम्मा’ के जिस हक़ का उल्लेख इन आयतों में आता है वे ज़कात के अलावा हैं।
यही आयत “और उन (दौलतमंदों) के मालों में माँगनेवाले और वंचित का भी हक़ है।” (क़ुरआन, 51:19) किफ़ालते-आम्मा की इस्लामी धारणा का आधार है। इसका विस्तृत विवरण आयते-बिर्र (2:177) में मिलता है जो सूरा-2 बक़रा में है, जिसमें ज़कात का उल्लेख करने के बाद कहा गया है—“माल की मुहब्बत के बावजूद या अल्लाह की मुहब्बत की वजह से माल प्रदान करता है” और अपने ग़रीब रिश्तेदारों को और फ़ुलाँ-फ़ुलाँ को देता है। यह इसलिए है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) के शब्दों में वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए “यहाँ तक कि ‘कफ़ाफ़’ के दर्जे में सब मुसलमान बराबर हो जाएँ।” कोई मुसलमान ऐसा न रहे जिसको दर्जा ‘कफ़ाफ़’ भी मयस्सर न हो। पवित्र क़ुरआन में जो मक्की सूरतों के आरम्भ से इस तरह के इशारे हैं जैसे “जो यतीम का खाना देने पर नहीं उभारता”। यह उसी दर्जा ‘कफ़ाफ़’ की प्राप्ति को निश्चित बनाने के लिए है। यह बात मुस्लिम समाज के स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए कि वह यह प्रबन्ध रखे कि ये ज़रूरतें हर व्यक्ति की पूरी हो जाएँ।
कफ़ाफ़ के दर्जे में यों तो रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं, लेकिन कुछ इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘कफ़ाफ़’ और ‘हाजियात-अस्लिया’, इन दोनों को सामने रखते हुए पवित्र क़ुरआन और हदीसों के विभिन्न स्पष्ट आदेशों से यह निष्कर्ष निकाला है कि मौलिक आवश्यकताओं में शिक्षा, इलाज, सुख-शान्ति, न्याय का उपलब्ध होना और एक पारिवारिक जीवन के संसाधन भी शामिल हैं। ये सब ‘हाजियाते-अस्लिया’ का दर्जा रखते हैं। अगरचे ‘कफ़ाफ़’ के बाद ही उनका दर्जा आता है, लेकिन मात्र ‘कफ़ाफ़’ पर सन्तोष करना सम्भव नहीं है। यह इंसान के स्वभाव, विकासवादी स्वभाव और सभ्यता एवं संस्कृति की प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ है। इंसान का स्वभाव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करने और अपने मामलों को बेहतर-से-बेहतर बनाने का है।
यह वही बात है जिसको हज़रत शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इर्तिफ़ाक़ के लफ़्ज़ से याद किया है। हर इंसान और हर मानव समाज पहले इर्तिफ़ाक़ से, यानी सभ्यता एवं संस्कृति के आरम्भिक दर्जे से दूसरे दर्जों में जाना चाहता है। दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे में जाना चाहता है। इस काम के लिए शरीअत ने सीमा-रेखाएँ तय कर दी हैं। यह विकास या यह graduation शरीअत के नियमों और आदेशों के अनुसार होना चाहिए। अगर यह विकासवादी प्रक्रिया शरीअत के आदेशों के अनुसार है, नैतिकता और आध्यात्मिकता की सीमाओं के अधीन है तो फिर यह शरीअत की नज़र में पसंदीदा है।
ये ज़रूरतें और विशेष रूप से जो आरम्भिक तीन ज़रूरतें हैं, ‘कफ़ाफ़’ की जो ज़रूरतें हैं वे अगर पूरी न हों तो उसके नतीजे में निराशा पैदा होती है। निराशा पैदा हो तो निराश इंसान फ़्रस्ट्रेशन (कुंठा) का शिकार होता है। फ़्रस्ट्रेशन के परिणामस्वरूप अनगिनत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसलिए इन ज़रूरतों को पूरा करना, ख़ुद समाज के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। उन लोगों के स्थायित्व और सुरक्षा के लिए भी अपरिहार्य है जिनके पास संसाधन मौजूद हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, सुदूर अतीत की भी और निकट अतीत की भी। फ़्राँस की क्रान्ति का उदाहरण है, रूस की क्रान्ति का उदाहरण है। अनेक अन्य देशों के उदाहरण हैं। अभी कुछ वर्ष पहले रोमानिया की मिसाल है कि पिछड़े और ग़रीब वर्ग कड़ी प्रतिक्रिया और निराशा का शिकार हुए, और इसके नतीजे में वह सब नष्ट हो गया जो प्रभावकारी और शासक वर्गों ने काफ़ी समय के बाद प्राप्त किया था।
इसी तरह अगर धन-दौलत और उपभोगी वस्तुएँ ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध हो जाएँ, रोटी, कपड़ा, मकान और दूसरे भौतिक संसाधन ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को प्राप्त हो जाएँ तो इससे भी बहुत-सी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अधिक पैसा होने के कारण फ़ुज़ूलख़र्ची करनेवालों का वर्ग पैदा होता है। यह वर्ग नैतिक ख़राबियों का कारण बनता है। इसलिए इन दोनों में सन्तुलन की ज़रूरत है। सन्तुलन यह है कि हर व्यक्ति को मौलिक आवश्यकताएँ एक ख़ास सतह तक इस तरह प्राप्त हों कि वह सन्तुष्ट रहे। भोजन, दवाएँ, वस्त्र, घर, घर की ज़रूरतें, सवारी, शिक्षा, न्याय, कुछ फुक़हा ने लिखा है कि सफ़ाई का सामान, ये तमाम चीज़ें हर व्यक्ति को ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध हों, उसकी इतनी आय हो कि वह इन चीज़ों को प्राप्त कर सके। बाज़ार में ऐसे संसाधन मौजूद हों कि इन ज़रूरतों की प्राप्ति आसान हो जाए, तो फिर समाज सन्तुष्ट रहता है और इस सन्तुष्टि के नतीजे में कोई नैतिक बुराई या ऊहापोह पैदा नहीं होता।
राज्य की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी आर्थिक सुनियोजन भी है। आजकल सुनियोजन एक बहुत बड़ी कला है। सुनियोजन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। सुनियोजन पूँजीवाद में किस तरह होता है, साम्यवाद में कैसे होता था। ये वे मामले हैं जिनसे आज सुनियोजन के विशेषज्ञ बहस करते हैं। इस्लामी राज्य में योजना बनाते हुए राज्य को जो सिद्धान्त सामने रखने चाहिएँ उनमें सबसे पहला सिद्धान्त आर्थिक ज़िम्मेदारियों की सीमाबंदी है। राज्य को इजाज़त नहीं है कि वह आम लोगों के काम में अनुचित हस्तक्षेप करे। लोगों की आज़ादियों को छीन ले। लेकिन आज़ादी के नाम पर किसी को सरपट दौड़ने की इजाज़त भी न हो। हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हों, बाज़ार सबके लिए खुला हो, यह बात निश्चित बनाना आर्थिक सुनियोजन का मूल अंग है।
शरीअत ने ज़रिए रोकने का आदेश दिया है। ज़रिए रोकने से मुराद यह है कि उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाए, उन तमाम संसाधनों और साधनों को हतोत्साहित किया जाए जिनके नतीजे में बुराइयाँ पैदा हो रही हों या पैदा होने की सम्भावना हो। इसलिए जमाख़ोरी, नाजायज़ मुनाफ़ाख़ोरी, स्मगलिंग, नाजायज़ आय, धोखाधड़ी, छल-प्रपंच, इस तरह की तमाम ख़राबियों का रास्ता रोकना और रास्ता रोकने के लिए उचित निरोधी उपाय अपनाना, यह राज्य की ज़िम्मेदारी है और आर्थिक सुनियोजन का एक अंग होना चाहिए। इसलिए इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने मूल सिद्धान्त बनाया है कि “पहले चरण के तौर से जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर किया जाए। दूसरे मरहले में जो फ़ायदे या निहितार्थ हैं उनको प्राप्त किया जाए।” निहितार्थ को प्राप्त करने के लिए ख़राबी को दूर करना ज़रूरी है। कोई बेहतरी उस वक़्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक ख़राबी को दूर न किया जाए।
योजना बनाने से सम्बन्धित अधिकतर काम वे हैं जिनका सम्बन्ध मात्र अनुभव से और आधुनिक काल के प्रचलन से है। यह वह तत्वदर्शिता है जो मुसलमान की गुमशुदा पूँजी है। जहाँ मिले मुसलमान को उसे प्राप्त करना चाहिए। अत: जिन-जिन अर्थव्यवस्थाओं में योजना बनाना सफल रहा है, उन सफलताओं का जायज़ा लेना, उनके कारणों का निर्धारण करना और उन कारणों को अपनाना शरीअत की अनिवार्य अपेक्षा है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि माल और संसाधन अल्लाह तआला की अमानत हैं। माल की सुरक्षा शरीअत के उद्धेश्यों में से है। शरीअत के आदेशों के अनुसार माल बर्बाद करने की मनाही है। शरीअत में फ़ुज़ूलख़र्ची से रोका गया है, इसलिए कि यह भी माल का बर्बाद करना है। इसलिए संसाधनों को बर्बादी से रोकना और संसाधनों के बेहतर-से-बेहतर इस्तेमाल को निश्चित बनाना गहरे सुनियोजन के बिना सम्भव नहीं है। इसी तरह ख़र्चों को सीमाओं के अनुसार करना भी शरीअत के आदेशों में शामिल है।
शरीअत ने जिस तरह का समाज क़ायम करना चाहा है वह मात्र उपभोक्ताओं का समाज नहीं है। जब एक बार उपभोक्ताओं का-सा स्वभाव क़ायम हो जाए, consumerism का रवैया पैदा हो जाए तो यह ज़िंदगी के हर पहलू में सामने आता है। फिर यह भौतिक पैदावार तक सीमित नहीं रहता। दूसरों की तैयार की हुई चीज़ बैठे-बिठाए प्राप्त करना और संसाधन ख़र्च करके उसको ख़रीद लेना, यह रवैया जब जन्म ले-ले तो फिर यह नैतिकता और अक़ीदों (आस्था) और विचारधारा तथा सभ्यता एवं संस्कृति और शिक्षा, संस्थाओं, हर चीज़ में सामने आता है। दूसरों की बनी-बनाई चीज़ें ज्यों की त्यों अपना लेने का स्वभाव बन जाता है। दूसरों की पकी-पकाई बैठकर खाने की आदत बन जाती है। इसलिए मुस्लिम समाज को मात्र उपभोक्ताओं का समाज नहीं होना चाहिए। न भौतिकता के उपभोक्ताओं का, न वैचारिकता और सभ्यता के उपभोक्ताओं का। मुस्लिम समाज को तो बल्कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ दुनिया के लिए सोचा जा रहा हो। दुनिया को क्या देन इस्लाम की ओर से मिलनी चाहिए, इन देनों पर काम हो रहा हो। ‘तय्यिबात’ (अच्छी चीज़ें) क्या हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, इसपर ग़ौर हो रहा हो। ‘ख़बाइस’ (बुरी चीज़ें) क्या हैं, नापाक और गंदी चीज़ें क्या हैं, उनकी निशानदेही हो रही हो। ‘तय्यिबात’ को बढ़ावा दिया जाए, ‘ख़बाइस’ को रोका जाए। हलाल-हराम की पाबंदी को निश्चित बनाया जाए। ये सारे मामले क़ानून और नीति बनाए बिना सम्भव नहीं हैं।
आजकल राज्य की भूमिका मुद्रा नीति के बारे में मूलभूत हो गई है, लेकिन अतीत में भी इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने इसको नज़र-अंदाज़ नहीं किया। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने लिखा है कि राज्य की ज़िम्मेदारी यह है कि वह सिक्के जारी करे। सिक्का जारी करना इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की नज़र में राज्य की ज़िम्मेदारी है। प्रसिद्ध मुहद्दिस और फ़क़ीह इमाम नववी ने लिखा है कि राज्य के अलावा किसी और के लिए यह बात दुरुस्त नहीं है कि वह दिरहम और दीनार ढालने का काम करे। चाहे वे विशुद्ध ही क्यों न हों। इसलिए कि यह काम सरकार का है और सरकार ही अगर सिक्का ढालने का काम करेगी तो फिर यह काम धोखे और मिलावट और वज़न की कमी से पाक-साफ़ रहेगा। एक और जगह इमाम नववी ने लिखा है कि “इन-न ज़-र-बन-नुक़ूद मिन आमालिल-इमाम” यानी सिक्के ढालना और आजकल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि नोट जारी करना भी राज्य की ज़िम्मेदारियों में से है।
ज़ाहिर है अगर नोट जारी करना और सिक्के ढालना राज्य की ज़िम्मेदारी है तो जाली और खोटे सिक्कों की रोक-थाम भी राज्य की ज़िम्मेदारी है। एक प्रसिद्ध मालिकी फ़क़ीह हैं वंशरीसी जिनका पश्चिम से सम्बन्ध था। इन्होंने अपनी किताब ‘अल-मेयारुल-मग़रिब’ में लिखा है कि सरकार को यह चाहिए कि वह इस बात से ग़ाफ़िल न रहे कि बाज़ार में जाली दिरहम और मिलावटवाले सिक्के चल रहे हैं। सरकार उसको सख़्ती से रोके। जो लोग इस हरकत में संलिप्त हैं उनका पता लगाए और अगर वे पकड़े जाएँ तो उनको कड़ी सज़ा दे, इसलिए कि यह एक ऐसा धोखा है जो मात्र किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, बल्कि पूरे समाज के साथ है। अगर व्यक्ति को धोखा देना जुर्म है तो पूरे समाज को धोखा देना उससे भी बड़ा जुर्म होना चाहिए।
यह बात इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने पवित्र क़ुरआन की इस आयत से निकाली है जिसमें इरशाद हुआ है कि “लोगों की चीज़ों और माल और दौलत (की क़ीमत) कम न करो।” (क़ुरआन, 11:85) यह आदेश आम है। लोगों की चीज़ें औने-पौने ख़रीद लेना, खोटे सिक्के जारी करना, कम वज़न के दिरहम और दीनार से काम चलाना। किसी की क़ीमती चीज़ को कम क़ीमत क़रार देकर ख़रीद लेना। यह सब ‘बख़्स’ में शामिल है। आजकल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिक्के को डी-वेल्यू करना भी ‘बख़्स’ का एक प्रकार है। आपने बतौर सरकार के ज़िम्मेदार के मुझे पाँच हज़ार रुपये देने का वादा किया। इसके बाद सिक्के की क़ीमत कम कर के आपने पाँच हज़ार की क़ीमत ढाई हज़ार कर दी और मुझे पाँच हज़ार का नोट पकड़ा दिया।
मुझे जिस क़ीमत को पाने का हक़ था वह क़ीमत आपने मुझे अदा नहीं की। यह भी उपर्युक्त आयत के अर्थ में शामिल है। आजकल इस आदेश पर कार्यान्वयन का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस आदेश को आज की आर्थिक भाषा में स्थानांतरित कैसे किया जाए, यह विद्वानों के ग़ौर करने का सवाल है।
इमाम अहमद-बिन-हंबल (रह॰) ने कम वज़न के सिक्के जारी करने को या जाली रूप से चला देने को ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ (ज़मीन में बिगाड़ फैलाना) क़रार दिया है। और आपको मालूम है कि ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ की सज़ा पवित्र क़ुरआन में बहुत सख़्त है। सूरा-5 माइदा में बयान किए हुए आदेश के अनुसार ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ की सज़ा कुछ शक्लों में सज़ा-ए-मौत है। प्रसिद्ध मालिकी फ़क़ीह इब्ने-रुश्द की भी यही राय है जो जाने-माने दार्शनिक और चिन्तक इब्ने-रश्द के दादा थे, उनकी राय भी यही है कि जो व्यक्ति जाली सिक्के इस्लामी राज्य में जारी करता है या खोटे सिक्के बाज़ार में फैलाता है, वह ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ का अपराधी है। यह ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ उन लोगों के बारे में कहा गया जो सामूहिक रूप से और संगठित होकर यह काम कर रहे हों। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई एक-आध आदमी कभी जाली सिक्का किसी को अस्ली कह कर दे दे तो यह जुर्म तो है, लेकिन यह ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति जाली नोट छापने की मशीन लगा ले, कोई व्यक्ति जाली सिक्के ढालने का कारख़ाना बना ले तो यह जुर्म इन लोगों के नज़दीक ‘फ़साद फ़िल-अर्ज़’ है जिसकी सज़ा मृत्युदंड हो सकती है।
आजकल राज्य बड़े पैमाने पर जुर्माने वुसूल करते हैं। क्या इस्लामी राज्य में जुर्माना लगाया जा सकता है? कुछ फुक़हा का ख़याल है कि नहीं लगाया जा सकता, कुछ का ख़याल है कि लगाया जा सकता है। ‘ताज़ीर बिलमाल’ यानी आर्थिक सज़ा जुर्माने की शक्ल में दी जा सकती है या नहीं, यह मसला फुक़हा के बीच चर्चा का विषय रहा है। कुछ हदीसों से अंदाज़ा होता है कि जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है और अतीत में इसकी मिसालें हैं कि जुर्माने की सज़ा दी गई है। हज़रत अली-बिन-अबी-तालिब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने जमाख़ोरी करनेवालों के भंडार ज़ब्त करके सरेआम जलवा दिए। यह भी एक दृष्टि से ‘ताज़ीर बिलमाल’ की एक शक्ल है। इस तरह की मिसालें और भी हैं जिनसे उसका अंदाज़ा होता है कि इस्लामी राज्य दूसरी सज़ाओं के साथ ताज़ीरी सज़ा के रूप में जुर्माने के तरीक़े भी अपना सकता है।
इस्लामी शरीअत का एक आम सिद्धान्त यह है कि “अल-ख़िराज बिज़-ज़मान” यानी जिस चीज़ का फ़ायदा आप उठा रहे हैं उसका नुक़्सान भी आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ से लाभान्वित हो रहे हैं तो इससे सम्बन्धित ज़िम्मेदारियाँ भी आपको अंजाम देनी पड़ेंगी। इसी सिद्धान्त के तहत इस्लामी राज्य और इसके नागरिकों के दरमियान सम्बन्धों के कुछ पहलू भी इस नियम के तहत आते हैं।
अगर किसी व्यक्ति का कोई वारिस न हो, उसका कोई रिश्तेदार दूर का या क़रीब का मौजूद न हो, तो बैतुलमाल उसका वारिस होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के ज़िम्मे कोई क़र्ज़ हो और वह मर जाए, उसकी कोई छोड़ी हुई विरासत न हो तो उसका क़र्ज़ बैतुलमाल अदा करेगा। यह बात कई हदीसों में बयान हुई है। “जिस व्यक्ति ने कोई बोझ छोड़ा तो वह हमारे ज़िम्मे होगा” यानी राज्य उसको अदा करेगा।
राज्य की आर्थिक ज़िम्मेदारियों के बारे में जो कुछ हदीसों में आया है वह बहुत विस्तृत है। उसके आधार पर इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने बहुत-से आदेश बयान किए हैं। जिनसे यह अंदाज़ा होता है कि इस्लामी राज्य विशुद्ध आर्थिक मामलों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पवित्र क़ुरआन की वह प्रसिद्ध आयत जिसमें इस्लामी राज्य के कर्तव्य बयान किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि अगर हम मुसलमानों को ज़मीन में सत्ता प्रदान करें तो “वे ज़कात अदा करेंगे, अच्छाई का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।” (क़ुरआन, 22:41) यानी ज़कात अदा करने का प्रबन्ध करना, यह राज्य की मूल ज़िम्मेदारियों में से एक है। एक हदीस में है कि “जिसका कोई वली न हो, वारिस न हो, राज्य उसका वारिस होगा।” जिसका कोई देख-भाल करनेवाला न हो, राज्य उसकी देख-भाल करेगा, जिसका कोई पूछनेवाला न होर राज्य उसको पूछेगा। एक जगह आया है “अल्लाह और रसूल उसके वली हैं जिसका कोई वली न हो।” इसलिए जो राज्य अल्लाह और उसके रसूल का उत्तराधिकारी है वह उसका वली (संरक्षक) होगा जिसका कोई वली न हो। एक और हदीस में आता है कि “अगर कोई व्यक्ति मर जाए और इसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो क़र्ज़ का अदा करना मेरे यानी राज्य के ज़िम्मे है।”
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) का वह जुमला तो हम सबने सुना है, जिसमें इन्होंने फ़रमाया था कि अगर फ़ुरात के किनारे पर कोई बकरी मर जाए तो मुझे ख़तरा है कि कहीं मुझसे अल्लाह तआला उसके बारे में न पूछे कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि बकरी भूखी मर गई और उसको चारा न मिला। हज़रत उम्र फ़ारूक़ (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक बार अपने गवर्नरों को निर्देश दिए और उनमें से एक को लिखा कि “लोगों के घरों में वुसअत (विशालता) पैदा करो।” यानी लोगों को आवास खुले और आरामदेह उपलब्ध करो। या उनको इतने वेतन और संसाधन दो कि वे अपने घरवालों को अच्छी तरह से खिला-पिला सकें।
राज्य की ज़िम्मेदारी के हवाले से एक आख़िरी चीज़ का उल्लेख करके बात को ख़त्म करता हूँ। वह इस्लामी राज्य में वक़्फ़ का मामला है। यह इस्लामी इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक, सभ्यता सम्बन्धी, सांस्कृतिक और सामूहिक संस्था थी जिसमें राज्य की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। क़ानूनसाज़ी के द्वारा भी और नीति निर्धारण के द्वारा भी राज्य वक़्फ़ की संस्थाओं को बेहतर-से-बेहतर चलाने में मदद दिया करता था। आज के दौर में राज्य की ज़िम्मेदारियों के सन्दर्भ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले पेश आ रहे हैं जिनपर आजकल के फुक़हा को चिन्तन-मनन करना चाहिए। आज से पचास वर्ष पहले, साठ वर्ष पहले लोगों की बड़ी-बड़ी सम्पत्तियों को राष्ट्र के स्वामित्व में लेने के नाम पर ज़ब्त कर लेने की प्रवृत्ति पैदा हुई। मुस्लिम जगत् में बहुत-से लोग कम्युनिज़्म (साम्यवाद) की विचारधारा से प्रभावित हुए। दुनिया में कुछ मुस्लिम शासकों को समजावाद की और कोई बात पसंद आई हो या न आई हो यह बात ज़रूर पसंद आई कि अपने विरोधी राजनैतिक नेताओं की जायदादें, ज़मीनें, कारख़ाने और बड़ी-बड़ी सम्पत्तियाँ अपने क़ब्ज़े में ले ली जाएँ। चुनाँचे मुस्लिम जगत् के विभिन्न देशों में भी और पाकिस्तान में भी बड़ी-बड़ी सम्पत्तियाँ, कारख़ाने, व्यापारिक संस्थाएँ राष्ट्र के स्वामित्व में ले लिए गए। चूँकि राष्ट्र के स्वामित्व में लेनेवाले राजनैतिक लीडर ख़ुद किसी कारख़ाने के मालिक नहीं थे, इसलिए कारख़ाने और फ़ैक्ट्रियाँ कब्ज़ा लेने और हथिया लेने में तो बहुत उत्साहित रहे, लेकिन चूँकि ख़ुद उनका सम्बन्ध अंग्रेज़ों के पैदा किए हुए ज़मींदार वर्ग से था, इसलिए ज़मीनों के मामले में उन्होंने नर्मी दिखाई और ज़ाहिरी लीपा-पोती के अलावा बड़ी-बड़ी ज़मीनों को राष्ट्र के स्वामित्व में लेने का कोई काम नहीं किया।
लेकिन ख़ुद यह सवाल कि क्या राष्ट्र के स्वामित्व में लेना या नेशनलाइज़ेशन की यह प्रक्रिया शरीअत के अनुसार थी? इसके जो आर्थिक परिणाम निकले वे बहुत विनाशकारी निकले। पाकिस्तान की हद तक तो हम कह सकते हैं कि नेशनलाइज़ेशन की इस प्रक्रिया ने पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को तबाहो-बर्बाद करके रख दिया। शिक्षा को भी तबाह कर दिया, अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर दिया। जो साहब यह हरकत करके गए उनकी इस हरकत के दुष्परिणाम आज तक पूरी क़ौम भगत रही है। सरकारी मिल्कियत के नाम पर कृपा पात्र सरकारी अधिकारियों की बड़ी-बड़ी सरकारें और रजवाड़े क़ायम हो गए। वे कंपनियाँ, वे कारख़ाने, वे इंडस्ट्री, वे उद्योग, जो लोगों ने ख़ून-पसीने की कमाई से बनाए थे, जिसपर दिन-रात मेहनत की थी उनके मालिक एक दस्तख़त के द्वारा वहाँ से निकाल बाहर किए गए और ये सारी संस्थाएँ बैठे-बिठाए व्यावहारिक रूप से कृपा पात्र सरकारी अधिकारियों के स्वामित्व में चली गईं। परिणाम वह निकला जो आज आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है और इसको अपने पाँव पर खड़ा करने की जो भी कोशिशें हुईं वह सफल नहीं हुईं।
इसकी प्रतिक्रिया में अब वैसी ही एक और बुराई पैदा हो रही है। वह नई बुराई अब निजकारी के नाम से आ रही है। पश्चिमवालों ने ही राष्ट्र के स्वामित्व में लेने का नुस्ख़ा समझाया था। अब वहीं से निजकारी, ‘ख़सख़सा’ या प्राइवेटायज़ेशन के नाम से यह नया नुस्ख़ा समझाया गया है। चुनाँचे अब क़ीमती सरकारी जायदादें और संसाधन औने-पौने दूसरों के हाथों बेचे जा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के हाथों संवेदनशील संस्थाएँ बेची जा रही हैं। पाकिस्तान के ये क़ीमती संसाधन हम सबके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हैं। बिजली के उत्पादन के संसाधन, ऐसे-ऐसे इलाक़ों में मौजूद संसाधन जहाँ से पाकिस्तान का राजमार्ग गुज़रता है। बिजली के संसाधन विदेशी कंपनियों के हाथ औने-पौने दामों बेच दिए गए हैं। इतनी क़ीमत पर बेच दिए गए हैं जिससे कई गुना ज़्यादा मूल्य की उनके पास पहले से सम्पत्तियाँ मौजूद थीं। कुछ ऐसी संस्थाएँ बेची गईं जिनकी महीने की आय इस क़ीमत से ज़्यादा थी।
यह नुस्ख़ा चूँकि पूरे मुस्लिम जगत् में आज़माया जा रहा है। इसलिए दुनिया में हर जगह के विद्वान इसपर ग़ौर कर रहे हैं। अनेक लोगों ने इस विषय पर शोधपत्र भी प्रकाशित किए हैं। किताबें भी लिखी हैं। कुछ लोग ने फ़िक़्ह की राय को केवल कलात्मक दृष्टिकोण से देखा और इसको जायज़ समझा। कुछ और लोगों ने गहराई से इसकी सच्चाइयों, परिणामों और फलों पर ग़ौर किया, उनको यह बात नाजायज़ मालूम हुई। वस्तुस्थिति यह है कि अपने परिणाम की दृष्टि से यह एक नया उपनिवेशवाद है। यहाँ आए दिन नित-नई ईस्ट इंडिया कंपनियाँ क़ायम हो रही हैं, मुस्लिम जगत् में जगह-जगह विदेशी कंपनियाँ आकर बैठ रही हैं, जो मुसलमानों ही के संसाधनों से मुसलमानों ही के देश में बैठकर मुसलमानों ही के हाथों से काम लेकर वे उद्धेश्य प्राप्त करेंगी जो आज से दो सौ वर्ष पहले विभिन्न विदेशी कंपनियों के द्वारा प्राप्त किए गए थे।
राज्य की ज़िम्मेदारियों में आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, एक ऐसी इस्लामी मार्केट की स्थापना भी है जिसपर काफ़ी समय से विचार-विमर्श भी किया जा रहा है और इसकी ओर बुलाया भी जा रहा है। आजकल का मुद्रा बाज़ार पूर्ण रूप से ब्याज आधारित संस्थाओं के कंट्रोल में है। मुद्रा बाज़ार के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह ब्याज आधारित कारोबार, ग़रर (धोखा) और क़िमार (जूआ) की विभिन्न शक्लें हैं। आज ऐसे इस्लामी बाज़ार की ज़रूरत है जहाँ इस्लाम के आधार पर काम करनेवाली व्यापारिक संस्थाएँ, इस्लामी दिशानिर्देशों पर काम का आरम्भ करनेवाले बैंक, ख़र्चे, इस्लामी व्यापारिक कंपनियाँ, शरीअत के आदेशों के अनुसार लेन-देन करें और मुद्रा बाज़ार के वे जायज़ उद्धेश्य पूरे करें जो मुद्रा बाज़ार से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन कामों के लिए विभिन्न मुस्लिम राज्यों को अपने अर्थशास्त्र और विकासवादी नीति में परिवर्तन लाने पड़ेंगे। राज्य किस हद तक मुद्रा बाज़ार को क़ायम करने में सहायक एवं सहयोगी हो सकता है, यह इस कला के विशेषज्ञों की ज़िम्मेदारी है कि वे बयान करें कि यह काम कैसे होना चाहिए।
मुद्रा बाज़ार की समस्या पर आजकल के विद्वानों ने बहुत विस्तार से चिन्तन-मनन किया है। इसपर अनेक किताबें भी लिखी गई हैं जिनमें यह बताया गया कि बेचने और ख़रीदने के दस्तावेज़ों का अगर बाज़ार हो तो उसके इस्लामी सिद्धान्त और आदेश क्या होने चाहिएँ। ‘औराक़े-मालिया’ (वित्तीय दस्तावेज़) को जब क्रय-विक्रय के लिए पेश किया जाएगा, उसके नियम एवं सिद्धान्त क्या होने चाहिएँ। ज़ाहिर है ये आदेश और क़ानून शरीअत के अनुसार होंगे। उनमें ‘रिबा’ नहीं पाया जाता होगा। उनमें ब्याज नहीं पाया जाता होगा। ‘रिबा’ के आदेश की पूरी पाबंदी करते हुए जब औराक़े-मालिया का लेन-देन किया जाएगा तो वह बहुत हद तक इस लेन-देन से विभिन्न होगा जो आधुनिक बाज़ारों में किया जा रहा है।
इसी तरह जब ‘हिसस’ (शेयर्स) के क्रय-विक्रय की समस्या आएगी तो शेयर्स के क्रय-विक्रय में भी ‘रिबा’ के हराम होने के आदेश को सामने रखना पड़ेगा। अगर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स का क्रय-विक्रय हो रहा हो जिसके पास केवल नक़द रक़म मौजूद है तो उसके शेयर्स के क्रय-विक्रय के अर्थ ये हैं कि मुद्रा का क्रय-विक्रय मुद्रा के साथ हो रहा है जो केवल बराबर-सराबर के आधार पर ही हो सकता है, कमी-बेशी के आधार पर नहीं हो सकता। इसी तरह शेयर्स का वह क्रय-विक्रय जो आजकल प्रचलित हो गया है जिसमें फ़्यूचर सेल भी शामिल है, जिसमें विशेष शेयर्स भी शामिल हैं। उनके आदेश संकलित किए जाने ज़रूरी हैं।
ये सब वे आदेश हैं जो मुद्रा बाज़ार से सम्बन्ध रखते हैं, जिनके बारे में आजकल के फुक़हा ने तफ़सील से आदेश संकलित किए हैं। इस विषय पर किताबें भी लिखी गई हैं और इन संस्थानों के फ़ैसले और फ़तवे भी आए हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से इजतिहाद से काम लेकर आजकल की फ़िक़्ही और क़ानूनी तथा आर्थिक समस्याओं का जवाब दिया है। चुनाँचे राबिता आलमे-इस्लामी (Muslim World League) के मातहत जो फ़िक़्ह अकैडमी क़ायम है उसने अपनी बहुत-से प्रस्तावों में इन समस्याओं का जवाब दिया है। जिद्दा के इस्लामी संगठन ओआईसी के अधीन जो अन्तर्राष्ट्रीय फ़िक़्ह अकैडमी काम कर रही है उसने भी इन मामलों के बारे में बहुत विस्तार से राय दी है। उसके फ़ैसलों और प्रस्तावों में इन समस्याओं का विस्तृत जवाब मिलता है, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि आधुनिक काल के इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने सामूहिक रूप से क्या निषकर्ष निकाले हैं। उनकी सामूहिक सूझ-बूझ इस मामले में क्या कहती है। यह वे समस्याएँ हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से राज्य और राज्य के अधिकार से है।
Facebook: HindiIslamPage
X: HindiIslam1
Hindi Islam Waht's App Channel (New): Hindi Islam
Recent posts
-

आधुनिक काल की मुख्य वित्तीय एवं आर्थिक समस्याएँ : एक अवलोकन (लैक्चर-3)
18 December 2025 -

इस्लाम की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था मूल-अवधारणाएँ, महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा लक्ष्य (लैक्चर -2)
16 December 2025 -
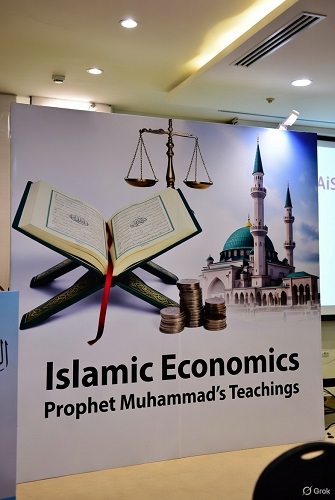
वित्त और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत पवित्र कुरआन और पैगंबर हजरत मोहम्मद (स0) की सुन्नत (शिक्षाओं एवं निर्देशों) की रोशनी में! (लैक्चर -1)
10 December 2025 -

इन्सान की आर्थिक समस्या और उसका इस्लामी हल
23 May 2022 -

आधुनिक पूंजीवादी समाज में शिक्षा, उपचार और न्याय
20 May 2022 -

ग़रीबी और अकाल का संबंध पूंजीवाद से
04 April 2022

