
आधुनिक काल की मुख्य वित्तीय एवं आर्थिक समस्याएँ : एक अवलोकन (लैक्चर-3)
-
अर्थशास्त्र
- at 18 December 2025
डॉ. महमूद अहमद ग़ाज़ी
अनुवादक : गुलज़ार सहराई
आज की चर्चा का शीर्षक है वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं और वित्तीय मुश्किलों का एक अवलोकन। इस चर्चा में उन महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों और माली समस्याओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जाएगा जो आज अर्थशास्त्रियों के लिए एक बड़े चैलेंज की हैसियत रखते हैं और जिनको सुलझाने, जिनका समाधान करने और जिनके रास्ते में आनेवाली रुकावटों को दूर करने के प्रयासों का ही नाम आजकल अर्थशास्त्र है। यह मुश्किलें क्या हैं, क्यों पैदा हुईं और इनका समाधान इस्लामी शिक्षा में क्या है, आज की चर्चा में संक्षेप के साथ इन्हीं समस्याओं पर बात की जाएगी।
आजकल की ये समस्याएँ बड़ी हद तक उस आर्थिक व्यवस्था की पैदावार हैं जो पश्चिम जगत् में पिछले कई सौ वर्षों के दौरान सामने आई है। जिसमें समय-समय पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन भी होते रहे हैं। इस व्यवस्था ने एक स्पष्ट रूप उन्नीसवीं सदी के मध्य से अपनाना शुरू कर दिया था। आर्थिक समस्याओं से निबटने का यह विशेष रूप जिसको कलात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। यह पश्चिमी आर्थिक विचारधारा की सबसे नुमायाँ प्रवृत्ति रही और बीसवीं सदी की चौथी दशक तक, बल्कि बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक जारी रही है। इसके बाद 1920 ई॰ के दौर से लेकर पश्चिम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लार्ड किंज़ के विचारों ने आर्थिक विचारों पर, आर्थिक विचारधारा पर और आर्थिक धारणाओं पर बहुत प्रभाव डाला। अर्थशास्त्र में बहुत परिवर्तन आए और इस नए अर्थशास्त्र को, इस नए संकलित अर्थशास्त्र को नव-कलात्मक अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र के नाम से याद किया जाता है। इस नए अर्थशास्त्र के नतीजे में जो मामले नुमायाँ तौर पर सामने आए हैं उनका सम्बन्ध आंशिक अर्थशास्त्र यानी micro economics से भी है और पूर्ण अर्थशास्त्र यानी macro economics से भी है।
पूर्ण अर्थशास्त्र यानी macro economics में राष्ट्रीय आय, मुद्रा और उसकी वास्तविकता, आन्तरिक और बाह्य व्यापार, उन्नति और विकास का मतलब, उसके प्रकार, नियोजन, आय में उतार-चढ़ाव (fluctuation), कर्मचारी और रोज़गार, धन-वितरण के मामले शामिल हैं। इन तमाम मैदानों में कुछ बड़ी-बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएँ पैदा हुई हैं, जिनके विभिन्न समाधान प्रस्तावित किए गए। इसी तरह आंशिक अर्थशास्त्र में जो समस्याएँ महत्वपूर्ण हैं उनमें मूल्य की अवधरणा और नज़रिया, उपभोक्ताओं का रवैया, आय और ख़र्च में सन्तुलन और पारिश्रमिकों की समस्याएँ शामिल हैं। इन समस्याओं से सम्बन्धित भी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ सामने आई हैं जिनपर कुछ लोगों ने चर्चा की है। इससे पहले उल्लेख किया जा चुका है कि एक विशेष धारणा जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था में पैदा हुई है, जिसपर मुस्लिम अर्थशास्त्रियों ने भी विस्तृत चर्चा की है, वह वस्तुओं या सेवाओं या संसाधनों की अतिरिक्त कमी का मामला है। यह अतिरिक्त कमी relative scarcity कहलाती है। इससे मुराद यह है कि जो संसाधन दुनिया में मौजूद हैं वे कम हैं, उनके मुक़ाबले में इंसानों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। इन ज़रूरतों को, इन सीमित संसाधनों की मौजूदगी में कैसे पूरा किया जाए, कैसे सब इंसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो अर्थशास्त्रियों के ध्यान का केन्द्र रही है।
मुस्लिम अर्थशास्त्रियों में कुछ लोग इससे मतभेद करते हैं। वे इस स्वघोषित कमी को कोई तयशुदा चीज़, या वास्तविकता क़रार नहीं देते, बल्कि मात्र पश्चिमी धारणाओं, बल्कि कल्पनाओं की एक शाखा समझते हैं, जिससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है। इसके विपरीत कुछ और अर्थशास्त्रियों ने इस धारणा से सहमति व्यक्त की है, उदाहरणार्थ हमारे विद्वान मित्र और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अबदुर्रहमान यसरी, इसको एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा समझते हैं। उनका ख़याल है कि आधुनिक ज्ञानपरक शोध ने यह ऐसी धारणा तलाश की है जो एक वास्तविकता की निशानदेही करती है और उसको बतौर वास्तविकता ही के देखना चाहिए। इस वास्तविकता को उनके ख़याल में, अब किसी नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं और उनको कैसे पूरा करना चाहिए।
बहरहाल यह एक समस्या थी जो मुसलमान अर्थशास्त्रियों के ध्यान का केन्द्र भी रही है। चूँकि उसका सम्बन्ध पूरी अर्थव्यवस्था से है, इसलिए मैंने उसकी ओर भी इशारा करना ज़रूरी समझा। इसका बड़ा गहरा सम्बन्ध लाभ की धारणा से भी है। यानी उपयोगिता या लाभ या यूटीलिटी क्या है। यह नव-कलात्मक अर्थशास्त्र की एक तस्वीर है। इससे मुराद हर वह गतिविधि है जो कोई भलाई पैदा करे और हर वह गतिविधि जो लाभ पैदा करे, वह उत्पादन गतिविधि है।
यहाँ लाभ से मुराद हर वह चीज़ है जिसको आम लोग या उनकी एक बड़ी संख्या अपने लिए लाभप्रद समझती हो। यह उपयोगिता या लाभ वह है जिसको आम आदमी अपने लिए उपयोगिता या लाभ समझते हों। यहाँ उसके नैतिक परिणामों या सामूहिक उद्धेश्यों से बहस नहीं है। इसलिए कि वित्तीय मामलों का नैतिक पहलू पश्चिमी नव-कलात्मक अर्थशास्त्र के कार्यक्षेत्र से बाहर है। इसलिए पश्चिमी अर्थशास्त्र में नैतिक मामलों से बहस नहीं होती। एक थोड़ी-सा बदलाव नव-क्लासिकी धारणा में पैदा हुआ है, वह यह कि इससे पहले यानी बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक तक विशुद्ध भौतिक वस्तुओं को उत्पादन गतिविधि का केन्द्र समझा जाता था और हर वह गतिविधि जिसके नतीजे में कोई भौतिक चीज़ सामने आए, सिर्फ़ उसी को उत्पादन गतिविधि कहा जाता था। लेकिन अब न्यू-क्लासिकी धारणा के अनुसार लाभ और फ़ायदे भी और सेवाएँ भी इसमें शामिल हो गई हैं। सेवाएँ, लाभ और मुनाफ़ा ज़ाहिर है भौतिकता से परे की चीज़ें हैं। भौतिकता से परे जो भी कुछ है, अगर वह इंसानों के लिए लाभकारी है या इंसानों को पसंद है तो फिर वह उत्पादन गतिविधि है। यहाँ भी नैतिक और धार्मिक दृष्टि से देखना ग़ैर-ज़रूरी है। धार्मिक दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, पश्चिमी अर्थव्यवस्था को इससे सरोकार नहीं है। अगर इंसानों की एक संख्या उसमें दिलचस्पी रखती है, उसपर पैसा ख़र्च करना चाहती है, उसको प्राप्त करना चाहती है तो उसको उपलब्ध करना एक व्यापारिक और उत्पादन गतिविधि है।
ज़ाहिर है यह बात इस्लामी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। इस्लामी अर्थशास्त्र तो दरअस्ल एक नैतिक अर्थशास्त्र है जिसमें ‘क़िस्त’ यानी वास्तविक न्याय पर ज़ोर दिया गया है। इसमें ‘एहसान’ (उपकार) और ‘ईसार’ (त्याग) की नसीहत भी की गई है। ज़ाहिर है ‘एहसान’ और ‘ईसार’ विशुद्ध धार्मिक मूल्य हैं। आजकल की धारणाओं के अनुसार व्यापार के मामले में उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन इस्लाम के इतिहास में व्यापार और नैतिकता, व्यापार और धार्मिक धारणाएँ हमेशा साथ-साथ चली हैं। फिर शरीअत ने जगह-जगह नसीहत यानी शुभचिन्ता की शिक्षा भी दी है। शुभचिन्ता व्यापारिक साथी के लिए भी, शुभचिन्ता किसी ग्राहक के लिए भी। शुभचिन्ता हर इंसान के लिए और अल्लाह के बनाए हर प्राणी के लिए हर वक़्त सामने रखना शरीअत की शिक्षा का मूल अंग है। व्यापार में शुभचिन्ता यह है कि मामले आपसी सहमति से हों।
सारांश यह कि इस्लामी अर्थव्यवस्था को नैतिकता और धार्मिक धारणाओं से बिलकुल ही अलग-अलग कर देना शरीअत की नज़र में स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत बहुत-से पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का मात्र ख़याल ही नहीं है, बल्कि यह बात उनके लिए अक़ीदा (आस्था) और विश्वास का दर्जा रखती है कि आर्थिक विकास और धार्मिक धारणाएँ एक साथ नहीं चल सकतीं। इन्होंने अपनी तमाम आर्थिक नीतियाँ और शोध इसी बुनियाद पर किए हैं। चुनाँचे अगर यह तय कर लिया जाए कि धार्मिक धारणाएँ और आर्थिक समस्याएँ एक साथ नहीं चल सकतीं तो उसके नतीजे में बहुत-से सवाल और समस्याएँ पैदा होंगी। ‘रिबा’ के अपरिहार्य होने का सवाल पैदा होगा। ग़रर (धोखा) पर आग्रह, furture sales की उपयोगिता और अपरिहार्य होना, काग़ज़ी करंसी, क़र्ज़ पर आधारित व्यापार और लेन-देन की तमाम शक्लें, यह सब वे मामले हैं जिनका एक मात्र उद्देश्य दौलत कमाना और दौलत में लगातार बढ़ोतरी करना है। दूसरी ओर धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब मामले ना-पसंदीदा और अस्वीकार्य क़रार पाते हैं। आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र ने मात्र नैतिक या वैचारिक सवाल ही नहीं उठाए हैं, उसने मात्र धार्मिक समस्याएँ ही पैदा नहीं कीं, बल्कि उसके नतीजे में बहुत-सी ऐसी समस्याएँ भी सामने आती हैं जो ख़ुद अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण समस्याएँ क़रार पाई हैं। और उनके समाधान पर दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न इलाक़ों में ध्यान दिया जा रहा है। इन समस्याओं का उल्लेख करने से पहले यह बात ज़ेहन में रखनी चाहिए कि आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र ही अब सोवियत यूनियन के पतन के बाद पश्चिम जगत्, बल्कि बड़ी हद तक पूरी दुनिया में अब एक मात्र आर्थिक व्यवस्था है। इस आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में अस्ल हैसियत पूँजीवादी धारणाओं को प्राप्त है, जिनकी उठान विशुद्ध शोषण पर आधारित है।
एक ज़माना था, 1940 ई॰ से लेकर 1980 ई॰ के दशक के मध्य तक, जब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कम्युनिज़्म के प्रोपेगंडे से बहुत प्रभावित था। ये लोग अपने को तरक़्क़ी-पसन्द (विकासवादी) कहने में ख़ुशी महसूस करते थे, गर्व से विकासवाद का इज़हार किया करते थे। और वे पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था के शोषणकारी होने की बात दिन-रात किया करते थे। वे यह बात कहते थकते नहीं थे। रात-दिन उनके लेखों में, उनकी ज़बानों पर, उनकी चर्चाओं में यही बात रहती थी कि पश्चिम की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सरासर शोषणकारी है। लेकिन यह अजीब बात है कि सोवियत यूनियन की टूट-फूट के बाद यह पूरा वर्ग न केवल परिदृश्य से ग़ायब हो गया, बल्कि उसने इन तमाम धारणाओं और विचारों को बयान करना भी छोड़ दिया, बल्कि उनको भुला दिया जो वह पश्चिम की शोषणकारी व्यवस्था के बारे में व्यक्त किया करते थे। उनमें से बहुत-से वे लोग हैं जो आज उसी ज़ोर-शोर से पश्चिमी धारणाओं के ध्वजावाहक बने हुए हैं और उन तमाम विचारों को उसी ज़ोर-शोर से दोहराते हैं जो आज अमेरिका, ब्रिटेन और इस शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के केन्द्रों से उठ रहे हैं और दुनिया के सामने आ रहे हैं, जो इस वर्ग के ख़याल में हर प्रकार की बुराई का केन्द्र था।
इससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था की आलोचना करनेवाले बहुत-से ज्ञानवान और विचारक अपने विचारों में इतने निष्ठावान नहीं थे, जितनी निष्ठा का वे दावा करते थे। इसकी वजह यह है ये दोनों व्यवस्थाएँ, प्राचीन कम्युनिस्ट व्यवस्था हो या आधुनिक पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था हो, प्रचलित व्यवस्था हो, इन दोनों का आधार नैतिक मूल्यों तथा अन्य आध्यात्मिक और मानवीय धारणाओं के इनकार पर थी। ये दोनों इस दृष्टि से अनैतिक व्यवस्था थे कि नैतिक मूल्यों को, प्रशासनिक, आर्थिक और सामूहिक मामलों में बिलकुल असम्बन्धित समझते थे। कम्युनिस्ट व्यवस्था में तो नैतिकता और धर्म की सिरे से ही कोई हैसियत नहीं थी, वहाँ तो उनको अफ़ीम समझा जाता था। लेकिन पश्चिमी दुनिया में जहाँ उन धारणाओं को कम-से-कम मौखिक या लिखित रूप से अफ़ीम नहीं समझा गया, वहाँ भी नैतिकता और धर्म को सामूहिकता में दख़ल देने की न पहले इजाज़त थी, न आज इजाज़त है।
इस धारणा या इस वैचारिक वातावरण का परिणाम यह निकलता है कि इंसान पर पूँजी की वरीयता क़ायम हो जाती है। बज़ाहिर यह एक वैचारिक बात मालूम होती है, लेकिन इसके बहुत-से आर्थिक, सामूहिक, और सांस्कृतिक परिणाम निकलते हैं जो बड़ी ख़राबियों पर आधारित हैं। हमारे देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित आर्थिक चिन्तक प्रोफ़ेसर शैख़ महमूद अहमद ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की इन कमज़ोरियों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और ख़ास तौर पर इंसान पर पूँजी की वरीयता के बारे में बड़ी ज्ञानपरक चर्चा की है।
दूसरी ख़राबी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से यह पैदा होती है कि इसमें सबसे पहला महत्व लाभ का होता है। तमाम आर्थिक गतिविधियों का पहला उत्प्रेरक लाभ और Profit को ज़्यादा-से-ज़्यादा करना बन जाता है। चुनाँचे maximization of profit (ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ कमाना), पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के मूल्य उद्धेश्यों में से है और आर्थिक गतिविधि के आधारभूत लक्ष्यों में से है। इसका परिणाम अवश्य यह निकलता है कि उपभोक्ताओं के हित नज़र-अंदाज़ हो जाते हैं। अगर पूरी व्यवस्था की उठान यह हो कि वह उद्योगपति का समर्थक है, वह भूमि के मालिकों का समर्थक है, राज्य और सरकार भी भूमि के मालिकों, पूँजीपतियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों की पीछे है तो उपभोक्ता के हित सिरे से नज़र-अंदाज़ हो जाते हैं और उनपर वह ध्यान नहीं दिया जाता जो होना चाहिए। उपभोक्ता का सम्बन्ध आम तौर पर कमज़ोर वर्ग से होता है। उपभोक्ताओं की अधिकांश संख्या उन लोगों की होती है जो बहुत कम संसाधन रखते हैं और हर दृष्टि से समाज में कमज़ोर समझे जाते हैं। व्यवस्था उनके हित का न केवल सुरक्षा नहीं करती, बल्कि एक हद तक उनके हितों के प्रति उदासीन हो जाती है। यह उदासीनता वैचारिक रूप से तो इतनी नहीं होती, लेकिन व्यावहारिक रूप से ज़रूर होती है।
इसके विपरीत इस्लामी शरीअत का स्वभाव यह है कि राज्य, राज्य के संसाधन और राज्य की पूरी शक्ति, सबसे पहले कमज़ोर और बेसहारा इंसान की मदद के लिए सामने आनी चाहिए। अगर समाज की शक्ति कमज़ोर शहरी के पीछे है तो यह क़ानून का सर्वोपरि होने और न्याय का प्रतीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आम इंसान, आम उपभोक्ता अपने को बेहैसियत समझता है, उद्योगपतियों की शक्ति, ज़मींदारों के प्रभाव और प्रभावकारी लोगों के प्रभावों के सामने बेबस मालूम होता है तो फिर यह शरीअत के पैमाने के दृष्टिकोण से क़ानून का वर्चस्व और न्याय नहीं है।
उपभोक्ताओं के ज़ेहन को एक ख़ास दिशा पर चलाने के लिए इश्तिहार-बाज़ी, पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अंग बन गई है। इतना अनिवार्य अंग बन गई है कि आज इश्तिहार-बाज़ी को एक कला समझा जाने लगा है। इसकी हैसियत एक बाक़ायदा ज्ञान की हो गई है। ऐसा ज्ञान जिसपर यूनिवर्सिटियाँ, शिक्षण संस्थाएँ और शैक्षिक गतिविधियों के केन्द्र शेष ज्ञान एवं कलाओं से कहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। छात्रों की बड़ी संख्या इसी इश्तिहार-बाज़ी की वजह से उन विभागों में अध्ययन के लिए आती है जहाँ से वे और अधिक इश्तिहार-बाज़ी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इश्तिहार-बाज़ी के विशेषज्ञों की यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती संख्या लाभ कमाने के उत्प्रेरकों को और अधिक मज़बूत करने में हिस्सा लेती है। उपभोक्ताओं के हित की असुरक्षा का और अधिक ज़रिया बनती है। इंसानों पर पूँजी की वरीयता को और अधिक मज़बूत बनाती है। इस सबके नतीजे में वर्गीय विभाजन गहरे से गहरा होता चला जाता है।
यह शिकायत आज दुनिया के हर देश में है कि वहाँ वर्गीय विभाजन फैल भी रहा है और गहरा भी हो रहा है। इस नारे के साथ कम्युनिज़्म उठा था और एक ऐसे वर्गीय विभाजन को जन्म देकर दुनिया से विदा हुआ जिससे बदतर वर्गीय विभाजन आज भी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है। वर्गीय विभाजन का अनिवार्य परिणाम धन के संकेन्द्रण की स्थिति में निकलता है। ज़ाहिर है जब एक वर्ग मज़बूत से मज़बूत-तर होता जाएगा, राज्य के तमाम संसाधन उसको प्राप्त होते जाऐंगे, इश्तिहार-बाज़ी के संसाधन उसको प्राप्त होंगे, इन हालात में उपभोक्ता अपने हित की सुरक्षा करने में और अधिक नाकाम होंगे और संसाधनों का बहाव प्रभावकारी वर्ग की ओर बढ़ता जाएगा, ग़रीब और दरिद्र वर्ग से कम होता जाएगा। यों ग़रीबों और बेसहारा वर्ग की ज़रूरतों से और अधिक उदासीनता और लापरवाही पैदा होती जाएगी, और यों यह वर्ग दिन-प्रतिदिन कमज़ोर से कमज़ोर-तर होता जाएगा। और प्रभावकारी वर्ग और अधिक प्रभावकारी और ताक़तवर होता जाएगा।
इस नकारात्मक स्थिति का एक परिणाम यह भी निकलता है कि उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल अधूरा होने लगता है। अगर उत्पादन के साधन का वितरण उचित हो, न्यायसंगत हो, तो हर व्यक्ति तक उत्पादन के साधनों का कोई न कोई हिस्सा पहुँचता है। वह इन उत्पादन के साधनों को इस्तेमाल भी करता है। इस तरह पैदावार के उपलब्ध साधनों का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल में आ जाता है। लेकिन अगर उत्पादन के साधन कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाएँ तो उन कुछ हाथों को तमाम संसाधन पूरे तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास इतना वक़्त ही नहीं होता कि बेकार और बे-इस्तेमाल संसाधनों पर पूरा ध्यान और उचित समय लगाएँ। यों इन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए जो संसाधन दरकार हैं वे भी कम पड़ जाते हैं। इसका अनिवार्य परिणाम यह निकलता है कि उत्पादन के साधनों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता।
संसाधनों का अन्यायपूर्ण वितरण जब भी होता है तो इससे धन का संकेन्द्रण भी पैदा होता है और आर्थिक उतार-चढ़ाव भी तेज़ी के साथ और बहुत अधिक आता है। जिसको fluctuation कहते हैं। यह बहुत निरन्तरता के साथ सामने आने लगता है। इस उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए सरकरें जो क़ानून लागू करती हैं वे अधिकतर अन्यायपूर्ण होते हैं। अन्यायपूर्ण क़ानूनों के नतीजे में और अधिक अन्यायपूर्ण विभाजन जन्म लेता है और यों यह सिलसिला जारी रहता है। आज वैश्विक स्तर पर भी जो क़ानून हैं वे बड़े अन्यायपूर्ण हैं। ये WTO और ISO और इस तरह के लुभावने शीर्षकों के तहत जो क़ानून दुनिया में बनाए गए हैं, वे आम तौर पर पूर्वी देशों और विशेष रूप से मुस्लिम जगत् के लिए आख़िरकार अत्यन्त विनाशकारी साबित होंगे।
मुझे तो स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि यह एक नया उपनिवेशवाद जन्म ले रहा है जो उन तमाम हितों और लाभों से लाभान्वित होगा जिनकी वजह से पश्चिम की औपनिवेशिक शक्तियाँ मुस्लिम जगत् में आई थीं, लेकिन अब उनपर उपनिवेशवाद का धब्बा नहीं होगा। इसको उपनिवेशवाद नहीं कहा जाएगा। उपनिवेशवाद कहलाई जाने की जो ख़राबियाँ या परिणाम हैं इससे वह मुक्त रहेगा। लेकिन लाभ उसको उपनिवेशवाद के पूरे-पूरे प्राप्त होंगे। इन तमाम मामलों का जो नकारात्मक प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा मुस्लिम जगत् पर पड़ेगा। इसलिए कि मुस्लिम जगत् में उनमें से बहुत-सी समस्याएँ पहले से भी मौजूद हैं। दो ढाई सौ वर्षों की पश्चिमी औपनिवेशिक स्थिति का परिणाम भी हैं और इससे पहले से मुसलमानों के पतन के दौर से भी कुछ समस्याएँ चली आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि मुसलमानों के पतन का दौर स्पष्ट रूप से दसवीं शताब्दी हिजरी के लगभग शुरू हुआ। पहले मुसलमान जड़ता का शिकार हुए, फिर उनके विकास में कमी आई, बल्कि उनका फैलाओ नैतिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक मैदानों में कम हो गया। और उनके आपस के मतभेद और आपस की जंगें उनके लिए बहुत-सी समस्याओं का कारण बनीं।
इस स्थिति के परिणाम भी पहले से मौजूद थे। धन-वितरण में असमानता थी। धन का संकेन्द्रण भी था। भुखमरी और बीमारी थी। अशिक्षा भी बहुत पैदा हो गई थी। कुछ देशों में साक्षरता शून्य थी। शोषण भी था। और कहीं-कहीं अमीर-ग़रीब का संघर्ष यानी polarization भी था। लेकिन ये सब समस्याएँ आम तौर से सीमित और बहुत आरम्भिक स्तर पर थीं। कहीं-कहीं उनका इज़हार था, कहीं-कहीं नहीं था। लेकिन जब पश्चिमी उपनिवेशवाद मुस्लिम जगत् में आया तो उन तमाम समस्याओं में न केवल शिद्दत पैदा हुई, बल्कि उनके साथ-साथ और भी अनगिनत समस्याएँ सामने आ गईं। वक़्त के साथ-साथ दौलत के अन्यायपूर्ण वितरण में वृद्धि होती गई।
पश्चिमी व्यवस्था की उठान और आधार पिछले कई सौ वर्ष से यही है कि दुनिया के संसाधनों का रुख़ पश्चिमी दुनिया की ओर रहे। सेवाएँ और महत्वहीन काम पूरब के लोगों से ले लिए जाएँ। लेकिन उनके परिणाम और विकास की निशानियाँ ज़्यादा शक्ति के साथ पश्चिमी दुनिया में सामने आएँ। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों का जायज़ा लिया जाए, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो यह वास्तविकता बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। यह आंकड़े विभिन्न आर्थिक समाचारपत्रों और कालमों में और कुछ साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। सन 1998 ई॰ में एक ऐसे ही सर्वे के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, उनमें यह बताया गया था कि सन 1998 ई॰ में लोगों की निजी और व्यक्तिगत ज़रूरतों पर जो रक़म पूरी दुनिया में ख़र्च की गई उसका 86 प्रतिशत दुनिया के मात्र 20 प्रतिशत लोगों ने ख़र्च किया। और शेष चौदह प्रतिशत दुनिया के 80 प्रतिशत इंसानों के हिस्से में आया। यह सिर्फ़ निजी ज़रूरतों पर ख़र्च की जानेवाली रक़म थी, यानी यह केवल वह रक़म थी जो लोगों की ख़ुराक, खाने-पीने, कपड़े, लिबास, इलाज पर ख़र्च हुई। इसमें सरकारों और संस्थानों के ख़र्चे और बड़ी-बड़ी कंपनियों के ख़र्चे शामिल नहीं हैं। अगर ये ख़र्चे भी शामिल किए जाऐंगे तो यह फ़र्क़ इससे भी कई सौ, बल्कि शायद कई हज़ार गुना ज़्यादा होगा।
ये असन्तुलन जो आज पूरब-पश्चिम के दरमियान पाया जाता है, यह मात्र संयोग नहीं है। यह इस आर्थिक व्यवस्था के अनिवार्य परिणाम हैं जो आज दुनिया में क़ायम है और जिसकी सुरक्षा और बचाव के लिए पश्चिमी दुनिया सब कुछ करने को तैयार है। आज फ़्री मार्केट इकॉनोमी और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पश्चिमी दुनिया के लिए दीन-धर्म का दर्जा रखते हैं। और पश्चिमी दुनिया उसके लिए इसी तरह की क़ुर्बानी देने को तैयार है जैसा कि निष्ठावान मुसलमान धर्म की सुरक्षा के लिए क़ुर्बानी देने को तैयार रहता है, बल्कि आज मुसलमानों में धर्म के लिए क़ुर्बानी देने का जज़्बा कम हो गया है। इसके मुक़ाबले में पश्चिमी दुनिया में अपनी इस व्यवस्था की सुरक्षा का एहसास दिन-प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। वे इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए देशों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। इंसानों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए आमादा हैं। देशों के संसाधनों पर क़ब्ज़े के लिए फ़ौजें उतारने में और बमबारी करने में उनको कोई संकोच नहीं है। इससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि पश्चिमी दुनिया अपनी इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए कहाँ तक जा सकती है।
पश्चिमी अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि इंसानों की हर भौतिक इच्छा को जायज़ इच्छा मानकर उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। यह केवल इसलिए है कि अर्थशास्त्र के मैदान से नैतिकता और धर्म के मूल्यों को निकाल बाहर किया गया है। किसी इच्छा को जायज़ इच्छा मानना या नाजायज़ इच्छा मानकर उसको रोकने की कोशिश करना यह नैतिकता और धर्म के आधार पर ही हो सकता है। वास्तविक और अवास्तविक ज़रूरतों में फ़र्क़ की असल बुनियाद नैतिकता ही है। जब वह ख़त्म हो जाए तो फिर वास्तविक और अवास्तविक ज़रूरतों में फ़र्क़ करना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन होता है।
इसके विपरीत औद्योगिक वस्तुएँ पैदा करनेवाले का हित और उत्पादन के साधनों के मालिक वर्गों के व्यापारिक निहितार्थ इसमें है कि वे अवास्तविक और फ़र्ज़ी ज़रूरतें पैदा करते चले जाएँ। अवास्तविक और फ़र्ज़ी ज़रूरतें पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि विज्ञापन के तमाम संसाधनों को इस्तेमाल किया जाए। संचार माध्यम पूर्ण रूप से उनके हाथ में हों, जैसा कि आज हो रहा है कि बड़े-बड़े पूँजीपतियों और पूँजीवादी कंपनियों के हाथ में बड़े-बड़े संचार माध्यम भी हैं। समाचारपत्र उनके कंट्रोल में हैं। टीवी के बड़े-बड़े नेटवर्क उनके पैसे से चल रहे हैं। बड़ी-बड़ी राजनैतिक पार्टियों के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ कारोबारी हित में वे साझेदार हैं। इन तमाम संसाधनों को इस्तेमाल करके और अधिक अवास्तविक और फ़र्ज़ी ज़रूरतें पैदा की जाती हैं।
जिन मामलों को इस्लाम के फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘कमालियात’ और ‘तहसीनियात’ (इनसे मुराद वे ख़र्चे हैं या वे तक़ाज़े हैं जिनको छोड़ देने में कोई कठिनाई या तकलीफ़ न हो) के नाम से याद किया था, उनको ज़रूरतों का दर्जा देना और बतौर ज़रूरतें के इंसानों को यह यक़ीन दिलाना कि इन चीज़ों के बिना उनकी ज़िंदगी कठिनाइयों का शिकार हो जाएगी यह पश्चिमी इश्तिहार-बाज़ी का मूल कर्तव्य है। नैतिक सीमाओँ और आध्यात्मिक मामलों को अर्थशास्त्र से ज़्यादा-से-ज़्यादा दूर रखना और नई-नई ‘कमालियात’ को पैदा करना फिर इन ‘कमालियात’ को ज़रूरतों का दर्जा देना, यह उद्योगपति के हित में भी है, यह व्यापारी के हित में भी है और यह हर उस व्यक्ति के हित में है जो नए-नए उत्पादों का कारोबार करता हो या उस कारोबार से लाभान्वित होता हो।
इस मुक़ाबले में इस्लाम को अभीष्ट यह है कि असीमित भौतिक इच्छाओं को सीमित रखा जाए। ज़रूरतों, ‘हाजियात’ और ‘कमालियात’ में फ़र्क़ किया जाए। ज़रूरतें, जिनकी पूर्ति अनिवार्य है, वे वाक़ई और वास्तविक ज़रूरतें हैं जिनपर मानव जीवन का दारोमदार हो, इंसान की सेहत का दारोमदार हो। इंसान की शिक्षा और इलाज का दारोमदार हो, जो इंसान की जायज़ दौलत की सुरक्षा के लिए, जायज़ संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य हों, ये वे ज़रूरतें हैं जिनको शरीअत स्वीकार करती है और उनकी पूर्ति के लिए आदेश देती है। ज़रूरतों के बाद दूसरा दर्जा इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने ‘हाजियात’ का बयान किया है। ‘हाजियात’ से मुराद वे मामले हैं जिनकी इंसानों को ज़रूरत तो होती है, लेकिन इस सतह पर नहीं होती जिस सतह पर वास्तविक और अपरिहार्य ज़रूरतें होती हैं। मिसाल के तौर पर हर व्यक्ति को सर छिपाने के लिए घर चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर हर व्यक्ति यह भी चाहता है कि उसका घर आरामदेह हो। आरामदेह घर की धारणा हर ज़माने के लिहाज़ से बदलती रहेगी। यह दूसरा दर्जा है जो ‘हाजियात’ कहलाता है। इसके बाद के दर्जे ‘कमालियात’ कहलाते हैं। ज़रूरतों और ‘हाजियात’ के बाद के जितने दर्जे हैं इसको इस्लामी विद्वानों ने ‘कमालियात’ या ‘तहसीनियात’ के नाम से याद किया है। एक व्यक्ति अपने घर को जितना बेहतर-से-बेहतर बनाना चाहता है, जितने ख़ूबसूरत अंदाज़ में बनाना चाहता है, जितने परिपूर्ण ढंग से इसके अंदर साधन-संसाधन उपलब्ध करना चाहता है, वह कर सकता है। बशर्तेकि वे जायज़ सीमाओं के अंदर हों, हलाल-हराम की सीमाओं के अनुसार हों और दूसरे इंसानों की ज़रूरतों और ‘हाजियात’ को नज़र-अंदाज़ करके उनको प्राप्त न किया गया हो। यह उसी वक़्त हो सकता है जब वास्तविक और अवास्तविक ज़रूरतों में अन्तर किया जाए। वास्तविक ज़रूरत वह है जो शरीअत की सीमाओं के अंदर हो, शरीअत के नियमों के अनुसार हो। जो इन नियमों के अनुसार नहीं है वह अवास्तविक है। फिर स्वयं वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति और पालन में भी शरीअत हदबंदी करना चाहती है। यह हदबंदी आम हालात में नैतिकता और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के द्वारा की जानी चाहिए और जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ क़ानून से भी काम लिया जाना चाहिए। शरीअत का अस्ल ध्यान इंसानों की मौलिक आवश्यकताएँ पूरी करने पर है। हर इंसान को ‘कफ़ाफ़’ (गुज़ारे) के अनुसार ज़रूरतें उपलब्ध हो जाएँ, यह शरीअत का मूल्य उद्देश्य है। इसलिए राज्य के आम संसाधनों का बहाव आम आदमी के कल्याण की ओर होना चाहिए और आम आदमी की ज़रूरतों की पूर्ति राज्य की सर्वप्रथम प्राथिमकता होनी चाहिए। अगर राज्य एक सीमित वर्ग की ‘कमालियात’ पर अपने अधिकांश संसाधन ख़र्च कर दे और अधिकांश आबादी की ज़रूरतों और ‘हाजियात’ को नज़र-अंदाज़ कर दे तो यह शरीअत के आदेशों का उल्लंघन होगा।
पश्चिमी अर्थव्यवस्था के इस वर्चस्व की वजह से आम तौर पर, और इस्लामी आदेशों को नज़र-अंदाज़ करने की वजह से विशेष रूप से, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अनगिनत समस्याएँ पेश आई हैं। उनमें कुछ समस्याएँ तो वे हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के हर देश में पेश आई हैं या आ रही हैं। उनमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं और ग़ैर-मुस्लिम देश भी शामिल हैं। कुछ समस्याएँ वे हैं जो विशेष रूप से मुस्लिम देशों में पेश आती हैं। मुस्लिम देश बहुत-सी जटिल आर्थिक कठिनाइयों का शिकार हैं जिनकी वजह यह है कि मुस्लिम समाजों के स्वभाव, प्रवृत्ति और अंदाज़ को नज़र-अंदाज़ करके कुछ ऐसे समाधान सुझाए जा रहे हैं जिनको मुस्लिम समाज का स्वभाव स्वीकार नहीं करता। पिछले कमो-बेश एक सौ वर्ष से यह कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी शिक्षा और प्रोपेगंडे के द्वारा आम लोगों को यह समझा दिया जाए और आम जनता को इन समाधानों के स्वीकार करने पर आमादा किया जाए। लेकिन परिणाम अभी तक कम-से-कम पिछले सौ डेढ़ सौ वर्ष से यही है कि मुसलमानों में अभी तक काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्होंने इन तमाम कोशिशों और भौतिक प्रेरकों के बावजूद अपने को इस पूरी व्यवस्था से अलग रखा हुआ है।
यह बात हममें से अक्सर की जानकारी में है कि ख़ुद हमारे देश में बहुत-से व्यापारी और उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी बैंक से लेन-देन नहीं किया। उन्होंने कभी न ब्याज दिया है, न लिया है। उन्होंने अपने कारोबारी मामलों में कभी भी शरीअत के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे बीसियों लोग हैं जिनका करोड़ों का कारोबार है। लाखों का कारोबार करनेवाले तो और भी ज़्यादा हैं। इससे यह अंदाज़ा होता है कि अभी तक मुस्लिम जगत् में पश्चिमी आर्थिक धारणाओं को और लेन-देन के तौर-तरीक़ों को सौ प्रतिशत स्वीकार्यता इस तरह की प्राप्त नहीं हुई जिस तरह की दूसरे पश्चिमी और ग़ैर-मुस्लिम देशों में प्राप्त हुई है।
इसका एक छोटा-सा परिणाम यह भी निकला है कि कुछ मुस्लिम देशों में, एक ही समय में दो अर्थव्यवस्थाएँ चल रही हैं। यह बात बहुत नुमायाँ है कि एक भूमिगत अर्थव्यवस्था है और एक धरती के ऊपरवाली अर्थव्यवस्था है। दोनों का फैलाव कुछ विशेषज्ञों के कथनानुसार बराबर-बराबर है। भूमिगत अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों में काफ़ी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो शरीअत के आदेशों का लिहाज़ रखते हैं। शरीअत के आदेशों की पैरवी करते हैं और जिस हद तक उनको शरीअत के आदेशों का ज्ञान है उस हद तक उनकी पैरवी करने की कोशिश भी करते हैं।
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया में जिन समस्याओं का सामना है, जिनका समाधान पश्चिमी धारणाओं के अनुसार करने की समय-समय पर कोशिशें भी की जाती हैं, जो अव्वल तो सफल नहीं हैं और अगर सफल हैं तो यह सफलता मात्र आंशिक है। इन समस्याओं में कुछ बहुत नुमायाँ हैं। इन सबसे नुमायाँ समस्याओं में निम्न जीवन स्तर और उत्पादन की कम सतह भी शामिल है। पैदावार का आज की दुनिया में जो स्तर है, दुनिया के विकसित देशों में पैदावार की जो सतह है, उससे बहुत कम सतह है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त है। पैदावार की इस कम सतह के बहुत-से कारण भी हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा चुका है। अलबत्ता एक बड़ा कारण उपभोक्ताओं का आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होना भी है। जब उपभोक्ता आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होगा, निर्धन होगा तो वह बड़े पैमाने पर उत्पादन की ख़रीदारी के लिए कैसे तैयार होगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन की बिक्री करने के लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ताओं के पास संसाधन हों। उपभोक्ताओं का वर्ग मज़बूत हो, और धन का वितरण न्यायपूर्ण हो। अगर उपभोक्ता सारे के सारे निर्धन और दरिद्र हों तो फिर पैदावार की सतह ऊँची भी हो तो उस समाज के लिए बेकार है।
बेरोज़गारी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की एक वैश्विक समस्या है। बेरोज़गारी खुली भी होती है और छिपी भी होती है। खुली बेरोज़गारी तो सबको नज़र आ जाती है, लेकिन छिपी बेरोज़गारी बहुत-से लोगों को नज़र नहीं आती। यह खुली और छिपी बेरोज़गारी जिसमें दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, यह भी पश्चिम की आर्थिक व्यवस्था का अनिवार्य तक़ाज़ा है। पश्चिमी देशों में आए दिन बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी की शिकायतें सुनने में आती हैं। लाखों कर्मचारियों को बड़ी-बड़ी कंपनियाँ Lay off (छंटनी) कर देती हैं, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी बढ़ जाती है। वे ऐसा क्यों करती हैं? वे इसलिए करती हैं कि उनको अचानक किसी ऐसे वित्तीय संकट का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से वे कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या का बोझ नहीं उठा सकतीं।
ऐसा अचानक वित्तीय संकट क्यों पैदा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन कंपनियों का सारा कारोबार अवास्तविक अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। मात्र काग़ज़ों में कर्ज़ की रक़म बढ़ती चली जाती है। काग़ज़ों में आय और लाभ की रक़म में बढ़ोतरी होती जाती है। वास्तविक पैदावार या वास्तविक सिद्धान्त या उपलब्ध वस्तुएँ और पूँजियाँ बहुत कम वुजूद में आती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक ग़ुब्बारे में गुंजाइश होती है हवा भरती रहती है, भरा हुआ नज़र आता है। अगर किसी वजह से इसमें ज़रा-सा भी छेद हो जाए तो यह बहुत छोटा-सा छेद इस पूरी हवा को बहुत जल्द निकाल देता है।
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक आम स्थिति यह भी देखने में आती है, वे कच्चे माल के निर्यात की समस्याओं से दोचार रहती हैं। उनके यहाँ केवल आर्थिक उत्पादन और कच्चे माल के निर्यात पर दारोमदार है। यह कच्चा माल जो बहुत औने-पौने दामों विकसित देशों को निर्यात किया जाता है। वहाँ से जब तैयार होकर आता है तो इन्हीं पूर्वी देशों में उसकी कई गुना क़ीमत हो जाती है। यह वर्षों से हम देख रहे हैं। इसकी मिसालें आए दिन विभिन्न देशों में देखने को मिलती हैं। इसका परिणाम आर्थिक बदहाली तो है ही, लेकिन एक परिणाम यह भी है कि विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। अगर आप केवल कच्चा माल पैदा करेंगे और इस कच्चे माल से उद्योगों की पैदावार की तैयारी किसी और देश में होगी तो आप उस देश पर निर्भर रहने के पाबंद हैं। वहीं आप अपना माल चाहे-अनचाहे भेजेंगे, वही आपसे अपनी शर्तों पर औने-पौने दामों ख़रीदेंगे तो आप उसको बेचेंगे, वर्ना आपके लिए आपका कच्चा माल बेकार है। अगर बाहर किसी देश में इसकी ज़रूरत है तो आप उसको बेचकर कुछ संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दूसरे देश आपकी कच्ची पैदावार आपसे लेने से इनकार कर दें तो आपके लिए उसका होना या ना होना बराबर है।
हम पाकिस्तानवालों को इसका बड़ा कटु अनुभव है। हमारे यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में हर वर्ष बड़े पैमाने पर पट-सन पैदा हुआ करता था। लेकिन इस पट-सन को इस्तेमाल करने के जितने कारख़ाने थे, वे हिंदुओं के पास पश्चिमी बंगाल या बिहार या ओडिशा आदि में थे। पाकिस्तान बनने के बाद वे सब कारख़ाने हमारे लिए व्यवहारतः बेकार और ख़त्म हो गए। अब अगर कहीं संयोगवश, उदाहरणार्थ दूसरे महायुद्ध के बाद कोरिया आदि में, पट-सन की माँग एक दम बढ़ गई तो बढ़ गई। और अगर बाद में वह उत्पादन लेने के लिए कोई तैयार न हुआ तो फिर उस कच्चे माल को देश के अन्दर ही औने-पौने बेच डालना काफ़ी समझा। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन हमारे प्यारे बंगाली भाई इससे सख़्त नाराज़ हुए। इन्होंने इसको पश्चिमी पाकिस्तानियों की नासमझी या ख़ुदग़रज़ी क़रार दिया।
ये निशानियाँ उस व्यवस्था की अनिवार्य अपेक्षाएँ हैं जो पहले भी सामने आती रहती हैं, बाद में भी सामने आती रहीं और आगे भी सामने आती रहेंगी। जब विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ सिर्फ़ कच्चे माल की निर्यात पर निर्भर करेंगी और उनका सारा दारोमदार विकसित देशों की ओर से ख़रीदारी पर होगा, तो इसका अनिवार्य परिणाम पूँजी में कमी के रूप में आएगा। पूँजी की कमी की स्थिति में टेक्नॉलोजी की कमी भी होगी। टैक्नॉलोजी की प्राप्ति के लिए पूँजी दरकार है, बड़ी मशीनरी के लिए पूँजी दरकार है। पूँजी नहीं होगी तो टेक्नॉलोजी भी नहीं होगी। टेक्नॉलोजी नहीं होगी तो आप वेल्यू ऐड करके कच्ची चीज़ों को बेच नहीं सकते। जब आप अपने तैयार किए हुए उत्पादन को बाहर बेच नहीं सकते तो विदेशी मुद्रा की कमी होगी। विदेशी मुद्रा की कमी होगी तो उसके नतीजे में इंडस्ट्री में फैलाव रुक जाएगा। जब इंडस्ट्री का फैलाव रुक जाएगा तो entrepreneur (उद्यमी) देश में कम हो जाऐंगे।
ये सारे परिणाम जो एक-दूसरे से जुड़े हैं एक-एककर सामने आते-जाते हैं। आप उसको विकासशील अर्थशास्त्र के फल कहें, बीमारीयाँ कहें, परिणाम कहें। बहरहाल ये वे परिणाम और फल हैं जो आज पूरी दुनिया में हर जगह नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम देशों में भी नज़र आ रहे हैं और ग़ैर-मुस्लिम देशों में भी नज़र आ रहे हैं।
इस स्थिति के कारणों पर अगर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो आजकल की एक मूल्य आर्थिक समस्या भी है, वह दौलत का अन्यायपूर्ण वितरण है। दौलत के अन्यायपूर्ण वितरण के यों तो बहुत-से कारण हैं। उनमें से कुछ की निशानदेही की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों का अगर उल्लेख किया जाए तो वे पाँच कारण हैं। ख़ुद पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को मुस्लिम जगत् में जी-जान से स्वीकार कर लेना उसका सबसे बड़ा कारण है। जब तक यह पूँजीवादी व्यवस्था जारी रहेगी, दौलत के अन्यायपूर्ण वितरण में और अधिक बढ़ोतरी होती जाएगी। दौलत की प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण वितरण की ओर ही रहेगी, न्यायपूर्ण वितरण की ओर नहीं होगी, इसलिए कि दौलत का अन्यायपूर्ण वितरण उस व्यवस्था की मूल आत्मा है। इसलिए इस व्यवस्था ने अपने तमाम ज़ाहिरी दावों के बावजूद Laissez faire के अर्थशास्त्र को बड़ी हद तक अब अभी बाक़ी रखा हुआ है। Laissez faire से मुराद यह था कि आर्थिक गतिविधि पर कोई बाहरी प्रतिबन्ध लागू न किए जाएँ, बाज़ार की व्यवस्था पर बाहरी प्रतिबन्ध न लगाए जाएँ। अगरचे आज पश्चिमी दुनिया का दावा है कि हमने स्वच्छन्द अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी है। लेकिन दरअस्ल ख़त्म नहीं की है। स्वच्छन्द अर्थव्यवस्था आज भी इसी तरह स्वच्छन्द है जैसे पहले थी। नैतिकता के प्रतिबन्ध पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं, बल्कि पहले शायद थोड़े-बहुत नैतिक प्रतिबन्ध हों, अब बिलकुल ख़त्म हो गए हैं। धार्मिक धारणाओं की सीमा-रेखाएँ जो रही सही थीं वे भी मिट गई हैं। जो प्रतिबन्ध आज लागू किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज कहा जा रहा है कि हमने स्वच्छन्द अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी है, ये सीमा-रेखाएँ वे हैं, जो ख़ुद व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य हैं। व्यवस्था को बदलने के लिए ये प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए। व्यवस्था की ख़राबियाँ दूर करने के लिए ये पाबंदियाँ नहीं लगाई गईं, बल्कि ख़ुद व्यवस्था को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। जिनकी बड़ी मिसाल आज WTO और ISO आदि के रूप में सामने आई है।
चूँकि इन सीमाओं ने इस व्यवस्था को और अधिक पुख़्ता किया है, और अधिक सुरक्षा प्रदान की है, इसलिए वैश्विक स्तर पर दौलत के अन्यायपूर्ण वितरण में और अधिक बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ख़ुद ब्याज या ‘रिबा’ जिसको शरीअत ने हराम क़रार दिया है, इसका स्वभाव और प्रवृत्ति भी यही है कि इसके नतीजे में दौलत के छोटे-छोटे भंडार इकट्ठा होकर बड़े भंडारों में परिवर्तित होते रहते हैं, और बड़े भंडार इकट्ठा होकर और अधिक बड़े भंडार में परिवर्तित हो जाते हैं। और आख़िरकार ये बड़े-बड़े भंडार कुछ पूँजीपतियों के कंट्रोल में आ जाते हैं। यह भी दौलत का अन्यायपूर्ण वितरण है।
इसके अलावा हमारे देश में विशेष रूप से जागीरदारी व्यवस्था इस अन्यायपूर्ण धन-वितरण और अन्यायपूर्ण संसाधन-वितरण को और सुदृढ़ करने का कारण बनी है। पूँजीपतियों या जागीरदारों के कुछ देशों में अलग-अलग वर्ग होते हैं। हमारे देश में अधिकतर स्थितियों में ये दोनों एक ही वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपने वफ़ादार सरदारोँ और प्रभावकारी लोगों को ज़मीनें देकर ज़मींदारों का एक वर्ग पैदा किया। इस ज़मींदार वर्ग ने देश के कृषि-संसाधनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इन कृषि-संसाधनों से काम लेकर उद्योग क़ायम किए। इन उद्योगों से काम लेकर बड़े-बड़े व्यापार अपने कंट्रोल में किए। यों देश के बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाएँ उनके प्रबन्धन में आ गईं। इस आर्थिक शक्ति से काम लेकर उन्होंने राजनैतिक शक्ति भी प्राप्त कर ली। इस वर्ग के बहुत-से लोग सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी शामिल हुए, और अब स्थिति यह मालूम होती है कि वह वर्ग जिसको अंग्रेज़ ने अपने औपनिवेशिक हित की ख़ातिर संसाधन प्रदान किए थे, जिसकी बदौलत चार हज़ार अंग्रेज़ पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करते रहे। वह वर्ग अब पाकिस्तान का स्थायी रूप से मालिक बन चुका है। वह वर्ग अब पाकिस्तान का स्थायी रूप से शासक भी बन गया है। वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में जो अंग्रेज़ नियुक्त थे उनकी संख्या चार-पाँच सौ से ज़्यादा नहीं थी। ये चार-पाँच सौ अंग्रेज़ जो साढ़े तीन लाख वर्ग मील पर शासक थे, उस वक़्त तीन साढ़े तीन करोड़ आबादी को कंट्रोल कर रहे थे, वे इसी वफ़ादार और जागीरदार वर्ग के ज़ोर पर कर रहे थे। इन तमाम समस्याओं का मूल, स्थायी और वास्तविक समाधान तो यह है कि इस्लामी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जाए।
इन तमाम आदेशों और क़ानूनों पर एक-एक करके कार्यान्वयन शुरू किया जाए जो शरीअत ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तावित किए हैं। इसके साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में सरकार की प्रभावकारी भूमिका, क़ानूनसाज़ी, पॉलिसी और निगरानी का रवैया, निगरानी की संस्था को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर इस्लामी अर्थव्यवस्था के आदेश पर कार्यान्वयन का यह काम क़ानूनसाज़ी और अदालती निगरानी के द्वारा हो तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस्लामी अर्थव्यवस्था प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ेगी और काम करेगी।
यह बात बहुत सुखद है कि पाकिस्तान की उच्च न्यायपालिका अभी तक इस वर्ग के प्रभाव और रुसूख़ से काफ़ी हद तक बाहर है जो अंग्रेज़ ने अपने वफ़ादारों पर सम्मिलित तैयार किया था और जिसकी वजह से अभी तक वही पॉलिसियाँ जारी हैं, वही शिक्षा-व्यवस्था जारी है, वही क़ानून काम कर रहे हैं और वही अदालती व्यवस्था जारी है जो अंग्रेज़ ने आज से दो सौ वर्ष पहले उपमहाद्वीप में परिचित कराई थी।
आर्थिक सुधारों की जब भी बात होगी और सम्भावित कार्रवाइयों का जब उल्लेख आएगा तो ब्याज का पूरी तरह ख़ातिमा धन के न्यायपूर्ण वितरण को यक़ीनी बनाने के लिए एक अपरिहार्य क़दम होगा। ‘रिबा’ का ख़ातिमा, क़ानूने-विरासत का प्रभावकारी ढंग से लागू होना और इस्लामी अर्थव्यवस्था के शेष आदेशों का लागू होना, ये तमाम काम दौलत के न्यायपूर्ण वितरण को यक़ीनी बनाने के लिए अपरिहार्य हैं।
शरीअत का एक आदेश बहुत महत्वपूर्ण है जिसका अगर तुरत-फुरत पालन किया जाए और कुछ सरकारी संसाधन उसके लिए तय कर दिए जाएँ तो उसके बहुत दूरगामी, सकारात्मक और सृजनात्मक परिणाम होंगे। शरीअत का आदेश है ‘एहयाए-मवात’ यानी मुर्दा ज़मीनों की आबादकारी का आदेश है। शरीअत का आदेश है, “जो व्यक्ति किसी ग़ैर-ममलूका (जिसका कोई मालिक न हो) और ग़ैर-आबाद ज़मीन को आबाद करे वह ज़मीन उसकी मिल्कियत समझी जाएगी।” अगर आज सरकार एक पॉलिसी ऐसी बनाए जिसके अनुसार वे तमाम ज़मीनें जो सरकार की मिल्कियत में हैं या किसी व्यक्ति की मिल्कियत में नहीं हैं, उनकी आबादकारी की इजाज़त आम लोगों को दे दी जाए, उसके नियम एवं सिद्धान्त बना लिए जाएँ। नियम एवं सिद्धान्तों का उद्देश्य इस काम में आसानी पैदा करना और इस काम को सही ढंग से करना हो, रुकावटें डालना और कंट्रोल करना मक़सद न हो तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। अगर सरकार ज़कात की रक़म से उन लोगों को प्रभावकारी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करे जो इन ज़मीनों को आबाद करना चाहते हों और उनका सम्बन्ध ज़कात हक़दारों के वर्ग से हो तो बहुत जल्द ऐसी ज़मीनें आबाद की जा सकती हैं जो आज ग़ैर-आबाद पड़ी हैं। शरीअत का एक आदेश है जिसको कुछ फ़ुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) ने एक फ़िक़ही नियम की शक्ल भी दी है, वह है “सरकार को जो अधिकार आम लोगों के मामले में प्राप्त हैं उन सबका दारोमदार और उनके औचित्य का आधार आम लोगों के हित पर है।”
धन-वितरण की इस नाबराबरी का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नकारात्मक परिणाम निकलता है वह आम तौर से धन के संकेन्द्रण के रूप में निकलता है। यों तो धन के संकेन्द्रण के और भी बहुत-से कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण धन-वितरण की व्यवस्था का अन्यायपूर्ण होना और संसाधनों के वितरण में नाबराबरी है। हमारे देश के हिसाब से जागीरदारी और राज्य की पॉलिसियाँ भी इसका बहुत बड़ा कारण हैं। विभिन्न प्रकार के एकाधिकार भी इसका ज़रिया हैं। इन कारणों का इलाज भी यही है कि राज्य की पॉलिसीयाँ न्यायसंगत हों। एकाधिकारों को हर सम्भव प्रयास ख़त्म किया जाए। जहाँ-जहाँ सम्भव हो क़ानून और न्याय के द्वारा एकाधिकार सम्बन्धी कोशिशों का ख़ातिमा किया जाए और ‘मुशारकाना’ (साझेदारी ढंग के) पूँजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। अर्थात् शोषण और पूँजी निवेश की वे शक्लें जिनमें पूँजी निवेश करनेवाले एक-दूसरे के साथ-साथ शरीक हों और व्यापार करनेवालों के साथ मुशारकत (साझेदारी) के सिद्धान्त पर व्यापार करें। यह सबसे बड़ा ज़रिया है धन-वितरण की प्रक्रिया में न्याय की आत्मा प्रविष्ट करने का और धन के संकेन्द्रण की धीरे-धीरे समाप्ति का।
सबसे बढ़कर इस्लाम का क़ानूने-विरासत फ़ौरी तौर पर अगर प्रभावकारी ढंग से लागू कर दिया जाए तो कुछ नस्लों के बाद ही यह भूमि संकेन्द्रण ख़त्म हो सकता है। अगर राज्य इस बात को यक़ीनी बनाए कि जो बड़ी-बड़ी जायदादें हैं, दौलत के बड़े-बड़े संसाधन हैं वे अस्ल मालिकों के मरने के बाद उनके वारिसों में निश्चित रूप से वितरित हो जाएँ तो उसके नतीजे में धन का संकेन्द्रण बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकता है।
पश्चिमी दुनिया ने धन के इस संकेन्द्रण को एक सिद्धान्त के रूप में अपनाया है। इसलिए वहाँ बहुत-सी ऐसी धारणाएँ और क़ानून मौजूद हैं जो धन के संकेन्द्रण को न केवल निश्चित बनाती हैं, बल्कि उसमें बढ़ोतरी का ज़रिया भी बनती हैं। उदाहरण के रूप में उनके यहाँ इस तरह का क़ानूने-विरासत नहीं है जिस तरह का इस्लामी शरीअत (धर्म विधान) में है कि दौलत समय-समय से क़रीबी रिश्तेदारों में व्यापक स्तर पर वितरित होती जाती है। पश्चिमी दुनिया में या तो यह बात व्यक्ति की अपनी समझ और अधिकार पर छोड़ दी गई है कि वह अपनी दौलत जिसके नाम करना चाहे कर दे। चुनाँचे वसीयत के नतीजे में भी संकेन्द्रित धन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है। कुछ लोग कुत्तों के नाम दौलत की वसीयत कर देते हैं, कोई बिल्ली के नाम कर देता है, कोई किसी के नाम कर देता है, कोई किसी के नाम कर देता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि क़रीबी रिश्तेदारों को, औलाद को, बूढ़े माँ-बाप को छोड़कर किसी वेश्या औरत के नाम पूरी जायदाद लिख दी। कुछ पश्चिमी देशों में विरासत का अगर कोई क़ानून है भी तो वह ‘तौरीसे-ज़िक्रे-अकबर’ का क़ानून है, यानी जिस व्यक्ति की जायदाद है, उसके वारिसों में जो निकटतम पुरुष रिश्तेदार है, बेटों में सबसे बड़ा बेटा, भतीजों में सबसे बड़ा भतीजा, भाइयों में सबसे बड़ा भाई, वह पूरी जायदाद का वारिस हो जाता है। न महिलाएँ वारिस होती हैं, न दूसरे रिश्तेदार वारिस होते हैं। यह बात आपको आश्चर्यजनक मालूम होगी कि आपने आज तक पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर महिलाओं के किसी भी प्लेटफ़ार्म को यह एतिराज़ करते नहीं सुना होगा कि Primogeniture का सिद्धान्त महिलाओं का अधिकार हनन है। पूरी जायदाद सबसे बड़े बेटे को या सबसे बड़े पोते को, या सबसे बड़े भाई को क्यों चली जाए, महिलाओं को क्यों न मिले। इसपर आज तक किसी महिला ने किसी संगठन ने, महिला अधिकारों के ध्वजावाहकों में से किसी ने एतिराज़ नहीं किया। हालाँकि यहाँ महिलाएँ पूर्ण रूप से वंचित हैं। पुरुष भी वंचित हैं। केवल एक व्यक्ति दौलत का वारिस बन रहा है। इसके विपरीत शरीअत पर एतिराज़ आए दिन आप सुनते-रहते हैं कि औरत का हिस्सा कुछ शक्लों में आधा क्यों है। हालाँकि जिन शक्लों में औरत का हिस्सा आधा है उनमें और शेष तमाम शक्लों में भी औरत पर कोई आर्थिक ज़िम्मेदारी शरीअत की व्यवस्था में नहीं है। बहरहाल क़ानूने-विरासत का व्यावहारिक रूप से लागू न होना भी धन के संकेन्द्रण के कारणों में से है।
फिर ब्याज पर आधारित अर्थव्यवस्था के नतीजे में भी धन-संकेन्द्रण और अधिक सख़्त होता चला जाता है। इस पूरे मामले का समाधान करने के लिए और धन के वितरण को हमेशा-हमेशा के लिए न्यायसंगत बनाने के लिए पूरी व्यवस्था पर भरपूर और आलोचनात्मक दृष्टिपात बहुआयामी परिवर्तन और सुधार की ज़रूरत है। टैक्सों की व्यवस्था पर न्यायसंगत और वास्तविकतावादी दृष्टिपात किया जाना चाहिए। तमाम वर्गों के लिए समानता की व्यवस्था होनी चाहिए। परोक्ष रूप से टैक्स कम-से-कम हों, अपरोक्ष रूप से ज़्यादा हों। फिर अगर ‘ज़कात’ और ‘उश्र’ (उश्र अर्थात् दसवाँ भाग। शरीअत की शब्दावली में खेत से पैदा अनाज का 10 प्रतिशत निकालकर ग़रीबों में बाँटना अनिवार्य है) को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए तो इससे बहुत फ़र्क़ पड़ सकता है, थोड़े-से समय में बहुत बड़ा परिवर्त आ सकता है।
शरीअत ने ज़कात और उश्र की व्यवस्था में अजीब प्रभाव रखा है कि कुछ वर्षों के अंदर-अंदर ग़रीबी का ख़ातिमा ही नहीं, भुखमरी का ख़ातिमा ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की आर्थिक गतिविधियों पर नुमायाँ तौर से सकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं, बशर्तेकि उस व्यवस्था को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाए। आज पाकिस्तान में उश्र की अदायगी न होने के बराबर है। जितना उश्र वुसूल होना चाहिए, उसका पाँच प्रतिशत भी शायद वुसूल नहीं होता। और कोई वुसूल करना भी नहीं चाहता। यही हाल ज़कात का है। ज़कात जितनी वुसूल होनी चाहिए उसका पाँच प्रतिशत भी वुसूल नहीं होती। जिस ज़माने में मेरा सम्बन्ध प्रशासनिक रूप से इन मामलों से था, मैंने कोशिश की थी कि कम-से-कम ज़कात की व्यवस्था को बेहतर और प्रभावकारी बनाया जाए, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। जिन लोगों के हित थे, जो लोग ज़कात की धारणाओं को मानते ही नहीं, उनके प्रभाव देश में बहुत गहरे हैं। इन्होंने इस रास्ते में रुकावट डाली और ज़कात और उश्र की व्यवस्था को प्रभावकारी और बेहतर बनाने की कोशिशों में असफलता का सामना करना पड़ा।
इसी अंदाज़ से पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था को नए सिरे से गठित करने की ज़रूरत है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसकी एक दिशा निर्धारित हो, जिसके लक्ष्य और उद्धेश्य निर्धारित हों, इन लक्ष्यों और उद्धेश्यों के लिए जो-जो काम अपरिहार्य हों उनपर सख़्ती से अमल किया जाए।
आजकल एक महत्वपूर्ण समस्या जो विभिन्न देशों, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े या कमज़ोर देशों, के सामने है वह ग़रीबी और भुखमरी की समस्या है। ग़रीबी और भुखमरी शरीअत की नज़र में अप्रिय चीज़ है। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कुफ़्र (ईश्वर का इनकार) और फ़क़्र (भुखमरी) दोनों से एक साथ पनाह माँगी है। الھم انی اعوذ بک من الکفر والفقر (अल्लाहुम-म इन्नी मिनल-कुफ़रि वल-फ़क़रि)। एक और हदीस में आता है कि कभी-कभी फ़क़्र (भुखमरी) कुफ़्र तक पहुँचा देता है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़क़्र के फ़ित्ने की बुराइयों से पनाह माँगी है।
ये फ़क़्र समाज में क्यों पैदा होता है? इसके कुछ कारण तो वे होते हैं जो इंसानों के बस से बाहर हों, उदाहरणार्थ प्राकृतिक आपदाएँ हैं। किसी इलाक़े की भौगोलिक स्थिति है, मौसम है। लेकिन कुछ कारण, बल्कि अधिकतर कारण वे हैं जो इंसानों के अपने पैदा किए हुए होते हैं। ज़्यादा-से-ज़्यादा लाभ कमाने की मुहिम, कुछ वर्गों को वंचित किए बिना सफल नहीं हो सकती। ख़र्चों की हदबंदी अगर न हो, लोग ख़ुद से शरीअत के आदेशों और नैतिक निर्देशों का पालन न करें और सरकार की ओर से भी नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों के पालन का कोई प्रबन्ध न हो तो फिर ख़र्चों की हदबंदी मुश्किल है। इस स्थिति का परिणाम यह निकलता है कि एक ख़ास वर्ग में दौलत का दिखावा और फ़ुज़ूलख़र्ची में मुक़ाबला शुरू हो जाता है। इस मुक़ाबले की तैयारी के लिए और एक-दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नाजायज़ दौलत की प्राप्ति शुरू हो जाती है। नाजायज़ दौलत की प्राप्ति की इन कोशिशों में वे लोग ज़्यादा सफल रहते हैं जो ज़्यादा प्रभावकारी हों। नतीजे में दौलत के संसाधनों का रुख़ उस वर्ग की ओर मुड़ जाता है जिसके पास संसाधन ज़्यादा हैं, जिसके पास ताक़त है, जिसके पास प्रभाव और पहुँच है।
फ़क़्र (भुखमरी) के कारणों में शहरों की आबादियों में अवास्तविक और ग़ैर-ज़रूरी बढ़ोतरी भी है। शहरी आबादियों में अनावश्यक बढ़ोतरी जहाँ बहुत-से नैतिक बिगाड़ों का ज़रिया बनती है, बहुत-सी सामूहिक ख़राबियों को भी जन्म देती है। जहाँ बहुत-सी प्रशासनिक समस्याएँ पैदा होती हैं वहाँ उसके आर्थिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ग़रीबी और भुखमरी में बढ़ोतरी होती है। अधिकतर शहरों के संसाधन सीमित होते हैं। आबादी उन संसाधनों से बढ़ जाए तो ग़रीबी तो अनिवार्य रूप से पैदा होगी। इसमें बढ़ोतरी भी होगी।
फिर वह वर्ग जो संसाधनों पर कंट्रोल रखता है वह आम लोगों की ज़रूरतों से मुँह फेरकर अपनी ‘कमालियात’ पर ज़ोर देना शुरू कर देता है। एक सीमित वर्ग की दिलचस्पी के लिए बेहतर से बेहतरीन संसाधनों, और बेहतर से बेहतरीन अर्थव्यवस्था उपलब्ध कर दी जाती है। दौलत और संसाधनों का बहाव इस ओर कर दिया जाता है। आम लोगों की ज़रूरतें नज़रों से ओझल हो जाती हैं। इसके नतीजे में भी और अधिक फ़क़्र पैदा होता है। इस समस्या का समाधान यही है कि शरीअत के इस क्रम को ध्यान में रखा जाए जो ज़रूरतों के बारे में शरीअत ने बताया है कि सबसे पहले आम लोगों की ज़रूरतों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। राज्य के संसाधनों और नीतियों का रुख़ यह हो कि शहरियों की जितनी मौलिक आवश्यकताएँ हैं उनको पहली प्राथमिकता प्राप्त हो। ज़रूरतों से मुराद वे ज़रूरतें हैं जो शरीअत की नज़र में ज़रूरतें हों। उनको पहले पूरा किया जाए। जब संसाधनों के अनुसार ज़रूरतें पूरे तौर पर पूरी हो जाएँ तो फिर जो शेष संसाधन हैं उनको ‘हाजियात’ पर ख़र्च किया जाए। ‘हाजियात’ से मुराद वे मामले होते हैं जिनके न होने की वजह से कोई मौलिक आवश्यकता बरबाद तो नहीं होगी। लेकिन आम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। उदाहरणार्थ बस्ती में पक्की सड़कें न हों तो लोग ज़िंदा रहेंगे, लोगों को ज़िंदा रहने में, आने-जाने में इलाज में, शिक्षा में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी, लेकिन मुश्किल बहुत होगी। अगर सड़कें मौजूद हों, संसाधन उपलब्ध हों तो लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इस तरह के मामले ‘हाजियात’ कहलाते हैं।
ज़रूरत और हाजत का निर्धारण परिस्थितियों और ज़माने के लिहाज़ से होता है। हो सकता है कि जो चीज़ें आज ज़रूरतों में गिनी जा रही हैं वे आज से सौ वर्ष पहले ‘हाजियात’ में शामिल की जाती हों। जो चीज़ें आज ‘हाजियात’ में शुमार की जा रही हैं, वे मुम्किन है कि आज से सौ वर्ष पहले ‘कमालियात’ में शामिल हों। इसलिए जिस दौर में फ़ैसला करनेवाले फ़ैसला करें, या संसाधनों का इस्तेमाल करनेवाले संसाधनों को इस्तेमाल करें उस दौर के स्तर और प्रचलित हालात के लिहाज़ से यह तय करना पड़ेगा कि ज़रूरतों में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। ‘हाजियात’ में कौन-कौन-से मामले शामिल होने चाहिएँ। और इन दोनों के बाद कौन से मामले हैं जिनकी हैसियत ‘कमालियात’ की है। जिनके लिए अगर संसाधन मौजूद हों तो ख़र्च किए जाएँ। न मौजूद हूँ तो ख़र्च न किए जाएँ। ‘कमालियात’ का मामला इस्लामी दौर में आम तौर से लोगों पर छोड़ दिया जाता था। राज्य के संसाधन आम तौर से ‘कमालियात’ पर ख़र्च नहीं होते थे। और अगर होते भी थे तो बहुत-सीमित सतह पर। राज्य के संसाधनों का अधिकतर भाग ज़रूरतों पर और ‘हाजियात’ पर ख़र्च होता था। अगर ऐसा हो और इसके साथ-साथ फ़ुज़ूल-ख़र्ची को सख़्ती से रोक दिया जाए, राज्य सादगी को बतौर एक नीति के अपनाए तो ग़रीबी और भुखमरी की समस्या बड़ी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है।
आजकल जब ‘फ़क़्र’ (भुखमरी) की बात होती है, ग़रीबी या संसाधनों की कमी की बात होती है तो बहुत-से लोग आबादी का मुद्दा उठाते हैं। पश्चिमी दुनिया में यह बात सबसे पहले राबर्ट मालथस ने उठाई थी। इसका मूल शोध यह था कि देशों की आबादियाँ जिस रफ़्तार से बढ़ती हैं, वह कृषि उत्पादन की रफ़्तार से बहुत ज़्यादा है। इसलिए आबादी को कम-से-कम रखने की कोशिश की जाए। मालथस का यह नज़रिया बहुत-सी कल्पनाओं पर आधारित है जिनका अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने गहरा बौद्धिक और आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। कुछ बड़े आलोचकों और अर्थशास्त्रियों का कहना यह है कि इन कल्पनाओं में से हर कल्पना विचारणीय है। ख़ुद बहुत-से पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने इन कल्पनाओं का कड़ी आलोचना का निशाना बनाया है।
आज पश्चिमी दुनिया के आंकड़े ही नहीं, बल्कि ख़ुद पूर्वी दुनिया के आंकड़े और आर्थिक प्रभाव सब मालथस की कल्पनाओं की ग़लती और झूठ के गवाह हैं। आंकड़ों ने, तथ्यों ने, आर्थिक इतिहास ने, पैदावार की रफ़्तार ने यह साबित कर दिया कि मालथस का नज़रिया बिलकुल ग़लत और ज्ञानपरक दृष्टि से निराधार था। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम के सेक्युलर, भौतिकवादी और भोगवादी ज़ेहन ने इन तमाम कल्पनाओं को दिलो-जान से स्वीकार कर रखा है।
मालथस के आबादी के नज़रिये पर पश्चिम में जिन लोगों ने आलोचना की उनमें जॉन स्ट्वार्ट मिल (John Stuart Mill) भी शामिल है। उसने ज्ञानपरक दृष्टि से, विशुद्ध पश्चिमी मापदंडों के अनुसार इस विचारधारा की बहुत-सी कमज़ोरियाँ बताईं। कार्ल मार्क्स ने भी इस नज़रिये का बड़ा मज़ाक़ उड़ाया है। आधुनिक मुस्लिम विचारक में सय्यद क़ुतुब, शैख़ ताहिर-बिन-आशूर, अबू-ज़ुहरा, मौलाना सय्यद अबुल-आला मौदूदी, अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी, डॉक्टर अबदुर्रहमान युसरी और दूसरे बहुत-से लोगों ने विशुद्ध ज्ञानपरक ढंग से आलोचना करके मालथस के दृष्टिकोण की ग़लती स्पष्ट की है।
पवित्र क़ुरआन ने स्पष्ट रूप से बताया कि रोज़ी में कमी-बेशी अल्लाह तआला की तत्वदर्शिता पर आधारित है। अल्लाह तआला ने इंसानों की रोज़ी में कमी-बेशी रखी है। लेकिन जहाँ तक संसाधनों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, वह हर इंसान के लिए बराबर है। यानी रोज़ी के संसाधनों तक पहुँच और access हर एक को बराबर प्राप्त है। फिर हर व्यक्ति अपने संसाधनों, अपनी प्रतिभाओं, अपनी मेहनत और कोशिश के अनुसार रोज़ी पाता है। दूसरी ओर पैदावार में बढ़ोतरी आबादी में बढ़ोतरी से बहुत ज़्यादा है। हर देश के आंकड़ों से यही ज़ाहिर होता है कि जितनी बढ़ोतरी आबादी में हुई है, इससे बहुत ज़्यादा पैदावार में हुई है। पाकिस्तान में 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी क्या थी और पैदावार क्या थी। आज पश्चिमी पाकिस्तान की, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, इसकी आबादी क्या है, पैदावार क्या है। और दूसरे देशों के आंकड़े पिछले पचास वर्ष के लिए जाएँ तो स्पष्ट हो जाता है कि यह धारणा निराधार थी। फिर रोज़ी के जो संसाधन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, जिनको अभी तक काम में नहीं लाया गया, वे अनगिनत हैं। अल्लामा इक़बाल के बक़ौल समुद्र के अंदर रोज़ी के क्या-क्या संसाधन मौजूद हैं। पहाड़ों के अंदर क्या कुछ मौजूद है। नदियों की तह में क्या है, जंगलों में क्या है, अभी तक तो उनमें से अधिकतर चीज़ों को किसी ने देखा भी नहीं।
दूसरी ओर यह एक हक़ीक़त है जिससे क़ुरआन और सुन्नत का कोई विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकता कि इस्लाम की प्रवृत्ति आबादी बढ़ाने की ओर है। बशर्तेकि आबादी की अधिकता किसी व्यक्ति के लिए निजी रूप से अव्यावहारिक साबित न हो। शरीअत ने निकाह को ‘सुन्नते-मुअक्कदा’ क़रार दिया, यानी उसपर ज़ोर दिया। दाम्पत्य जीवन को एकाकी जीवन से बेहतर और श्रेष्ठ क़रार दिया। अविवाहित लोगों की शादी कराने का निर्देश और उपदेश दिया। यह भी कहा गया कि अगर ये लोग फ़क़्रो-फ़ाक़े का शिकार हैं और इसलिए दाम्पत्य जीवन की ज़िम्मेदारियाँ उठाने से वे झिझक रहे हैं तो उनको यक़ीन दिलाओ कि अगर वे दरिद्र हैं तो अल्लाह तआला अपनी कृपा से उनको सम्पन्न कर देगा। फिर यह बात विशेष रूप से याद दिलाई गई कि जितने भी पैग़म्बर (अलैहिमुस्सलाम) थे वे सब-के-सब विवाहित जीवन गुज़ारकर गए हैं और पत्नियों और बच्चों के तमाम झमेले इन्होंने बर्दाश्त किए। और वह हदीस तो हमने कई बार सुनी है कि जिसमें अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि “मैं दूसरी क़ौमों के साथ मुक़ाबला करूँगा, उम्मत की कसरत (बहुलता) और क़िल्लत (कमी) के मामले में मेरी उम्मत दूसरी उम्मतों से अलग होनी चाहिए।” जहाँ ऐसे पैग़म्बर भी आएँगे जिनके साथ एक-एक या दो-दो ही पैरोकार होंगे, वहाँ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उम्मत संख्या और आबादी में सबसे ज़्यादा होगी।
यहाँ संख्या और आबादी की अधिकता का मतलब गुणवत्ता की क़ीमत पर संख्या में बढ़ोतरी नहीं है। बल्कि गुणवत्ता के साथ-साथ मात्रा में भी बढ़ोतरी दरकार और पसंदीदा है। गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए तो पूरे पवित्र क़ुरआन और हदीसों के दफ़्तर मौजूद हैं। जहाँ बेहतर से बेहतर नैतिकता, बेहतर से बेहतर ईमान, बेहतर से बेहतर किरदार, बेहतर से बेहतर कार्यकुशलता, बेहतर से बेहतर वैचारिक एवं शैक्षिक विकास के बारे में निर्देश मौजूद हैं, इन सबके साथ-साथ संख्या की दृष्टि से भी मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह इस्लाम को अभीष्ट है। ऐसा मालूम होता है कि पश्चिमी दुनिया ने मात्र अपनी ‘तहसीनियात’ और ‘कमालियात’ की ख़ातिर दुनिया की ‘ज़रूरतों व हाजियात’ को क़ुर्बान करने का चलन अपनाया हुआ है। इसलिए वे चाहते हैं कि दुनिया की आबादी कंट्रोल में रहे ताकि जो दर्जा ‘कमालियात’ और ‘तहसीनियात’ का उनको प्राप्त है वह प्राप्त रहे। इसमें कोई उनका मुक़ाबला करनेवाला न हो। कोई उन्हें compete करनेवाला न हो। और किसी देश की आबादी इस हद तक न जाए जो उनके लिए ख़तरा हो सके। यह बात इस मौज़ू से सम्बन्धित नहीं है, जिसपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह एक हक़ीक़त है। यह वास्तविकता है कि आबादी की समस्या एक महत्वपूर्ण राजनैतिक समस्या भी है। पश्चिमी दुनिया मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को राजनैतिक रूप से अपने लिए ख़तरा और अपने वैश्विक हित के लिए अनुचित समझती है।
यह बात मात्र संयोग नहीं है कि मुस्लिम जगत् के किसी देश के लिए आबादी में कंट्रोल के मामले में कभी सहायता की कमी नहीं हुई। विभिन्न देशों पर विभिन्न पाबंदियाँ लगती रहती हैं। बदतर से बदतरीन दौर में भी आबादी को कंट्रोल करने के लिए बाहर से कभी सहायता में कमी नहीं आई। ऐसा क्यों है? इसके जवाब पर ग़ौर किया जाए तो बहुत-से नुक्ते (Points) स्पष्ट हो जाते हैं। फिर यह दावा कि खानेवाले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, पैदावार कम है, तथ्यों के भी ख़िलाफ़ है। ख़ुद अमेरिका की कृषि पैदावार इतनी है कि वह अपने से कई गुना आबादी को खाद्य सामग्री उपलब्ध कर सकती है। लेकिन वहाँ भी आबादी-कम करने के सिद्धान्त को बतौर पॉलिसी के अपनाया गया है। मुस्लिम देशों में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केवल एक देश सूडान की पैदावार इतनी हो सकती है कि अगर वहाँ के तमाम संसाधनों को इस्तेमाल किया जाए तो पूरे मुस्लिम जगत् के लिए वह पैदावार काफ़ी हो सकती है।
आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सवाल यह रहा है कि क्या तलब (माँग) और रसद (सप्लाई) को पूर्ण रूप से आज़ाद छोड़ दिया जाए या उसको कंट्रोल किया जाए। इस मामले पर हर ज़माने के फुक़हा (इस्लामी धर्मशास्त्रियों) और मुफ़स्सिरीन (टीकाकारों) ने लिखा है। शैख़ुल-इस्लाम अल्लामा इब्ने-तैमिया (रह॰) ने तो इस समस्या पर एक पूरी किताब लिखी है। दूसरे कई लोगों ने भी इस समस्या पर ग़ौर किया और अपने चिन्तन-मनन के परिणाम को संकलित किया। इन सब लोगों के शोध की रौशनी में इस्लाम की राय यह मालूम होती है कि ज़रूरतों यानी तलब (माँग) को सम्भावित हद तक सीमित रखा जाए। कंट्रोल किया जाए। यह कंट्रोल प्रशिक्षण के द्वारा भी होगा, माहौल के द्वारा भी होगा, सामाजिक दबाव के द्वारा भी होगा और जहाँ अपरिहार्य हो वहाँ क़ानून के द्वारा भी होगा। दूसरी ओर रसद (सप्लाई) यानी ज़रूरतों की पूर्ति के मामले को नियमों का पाबंद बनाया जाए। न ज़रूरतें असीमित हों और न रसद असीमित हो। रसद को नियमों का पाबंद बनाया जाए और इसके द्वारा धन-वितरण की व्यवस्था को न्यायसंगत बनाया जाए और ज़रूरतों में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, वह ‘हाजाते-असलिया’ यानी इंसान की अनिवार्य मौलिक आवश्यकताएँ हैं, जिसके लिए फ़ुक़हा ने ‘कफ़ाफ़’ की शब्दावली इस्तेमाल की है।
‘कफ़ाफ़’ यानी ‘हाजाते-असलिया’ से मुराद मौलिक आवश्यकताएँ हैं। इन मौलिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास ये तीन चीज़ें तो सबके नज़दीक शामिल हैं। कम्युनिज़्म में भी दावा था कि ये चीज़ें हम उपलब्ध करेंगे। लेकिन फ़ुक़हा ने शरीअत का जो आदेश समझा उसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति एवं सुरक्षा और न्याय की स्थापना के साथ-साथ एक पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की उपलब्धता भी ‘हाजाते-असलिया’ में शामिल है। एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता में यह बात भी शामिल की गई है कि उसके पास केवल सिर छिपाने को मात्र एक घर ही न हो, बल्कि उसका एक परिवार भी हो जिसके साथ वह सुकून से रह सके, यानी जो अन्तर मकान और घर में है वह फ़ुक़हा ने महसूस किया। केवल मकान ही की ज़रूरत नहीं है हर व्यक्ति को घर की भी ज़रूरत है। एक ठिकाने की ज़रूरत है जहाँ उसको आध्यात्मिक और मानसिक तौर से सुकून मिल सके।
यही वजह है कि इस्लाम के ख़लीफ़ाओं ने बार-बार निर्धनों के वैवाहिक जीवन के ख़र्चे सरकारी संसाधनों से अदा किए। हज़रत उमर-बिन-अबदुल-अज़ीज़ का निर्देश था कि बैतुलमाल में वर्ष के अन्त पर जो संसाधन बच गए हों उन सबको ख़र्च करके जो अविवाहित युवक-यवतियाँ हैं उन सबकी शादी करा दी जाए। अगले वर्ष सूचना मिली कि और अधिक संसाधन बच गए हैं और सब विवाहित युवक-युवतियाँ विवाह की ज़िम्मेदारी से निवृत हो चुके हैं, आदेश दिया कि जितने ग़ैर-मुस्लिम युवक हैं उनके विवाह करवा दो। इससे यह अंदाज़ा होता है कि इस्लाम का स्वभाव ‘हाजाते-असलिया’ के बारे में क्या है।
ये जो वास्तविक ज़रूरतें होती हैं, ये अगर ज़रूरत से कम मयस्सर हों तो इस कमी से निराशा जन्म लेती है। जिसको पूरा भोजन नहीं मिलेगा उसके दिल में निराशा पैदा होने की अधिक सम्भावनाएँ हैं। जिसे ज़रूरत के अनुसार मकान और ठिकाना नहीं मिलेगा उसके दिल में निराशा की भावनाएँ पैदा होंगी। निराशा जब पैदा हो जाए तो इससे अनगिनत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। निराश इंसान से ज़्यादा ख़तरनाक मानवीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के लिए कोई और चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर ज़रूरतों की पूर्ति में संसाधनों की बहुतायत हो जाए तो यह भी समाज के लिए ख़तरा हो सकता है। ‘मुतरफ़ीन’ (सम्पन्न लोगों) की अधिकता भी सामाजिक मूल्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध होती है, यानी वे दौलतमंद जो अपनी बेपनाह दौलत के ख़र्च में किसी नैतिक नियम-क़ानून के पाबंद न हों। यह वर्ग जब किसी समाज में बढ़ जाए तो इससे अनगिनत सामाजिक ख़राबियाँ और नैतिक बुराइयाँ पैदा होती हैं। ऐसी बुराइयाँ जिसके नतीजे में समाज आख़िरकार तबाही का शिकार हो जाता है। इसलिए इन दोनों के दरमियान सन्तुलन होना चाहिए।
इस सन्तुलन का नाम शरीअत और इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था है। शरीअत ने इसके लिए एक मौलिक सिद्धान्त दिया है जो ‘मारूफ़’ का सिद्धान्त है। मारूफ़ से मुराद यह है कि जिस ज़माने के लिहाज़ से आप कोई पॉलिसी या क़ानून तय कर रहे हैं, उस ज़माने और उन हालात के अनुसार आप ज़रूरत और हाजत का निर्धारण करें। मैं यह बात पहले बता चुका हूँ कि बहुत-से ऐसे मामले जिनको आज ज़रूरतों में शामिल किया जाना चाहिए वे आज से सौ वर्ष पहले ज़रूरतों में शामिल नहीं समझे जाते थे। बहुत-सी ऐसी चीज़ें जो आज ‘हाजियात’ में समझी जाती हैं वे आज से पचास साल पहले ‘कमालियात’ मैं समझी जाती थीं। आइन्दा यह स्थिति और अधिक परिवर्तित होगी और होती रहेगी। इस्लामी अर्थव्यवस्था के लागू होने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात आवश्यक निपुणताओं की प्राप्ति भी है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) की राय में मुसलमानों के लिए इन तमाम निपुणताओं की प्राप्ति ‘फ़र्ज़े-किफ़ाया’ (वह कर्तव्य जो अगर कुछ लोग भी निभा दें तो सबकी तरफ़ से काफ़ी हो जाएगा, मगर यदि कोई भी न निभाए तो सब गुनहगार होंगे) है, जिनकी मुस्लिम समाज को ज़रूरत हो। आर्थिक आज़ादी के लिए, मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए, ज्ञान और शिक्षा को आम करने के लिए, इलाज की सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए और कफ़ाफ़ का प्रबन्ध करने के लिए विभिन्न कालों में विभिन्न निपुणताएँ अपरिहार्य होती हैं। इन तमाम उद्धेश्यों और ज़रूरतों के लिए जिन-जिन निपुणताओं की प्राप्ति अपरिहार्य है वे फ़र्ज़े-किफ़ाया हैं। ये निपुणताएँ हर दौर में बदलती रहेंगी। यह बात इमाम ग़ज़ाली, अल्लामा इब्ने-तैमिया और शाह वलियुल्लाह जैसे इस्लाम के बड़े विद्वानों ने लिखी है। जिस सिद्धान्त के आधार पर इन लोगों ने यह बात कही है, वह प्रसिद्ध फ़िक़ही सिद्धान्त है, “जिसपर किसी वाजिब (अनिवार्य) की प्राप्ति का दोरोमदार हो वह चीज़ भी वाजिब होती है।” चुनाँचे मुस्लिम समाज की रक्षा वाजिब है, फ़र्ज़ है। मुस्लिम समाज के बचाव के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों या जिन शक्तियों के मुक़ाबले में समुदाय का बचाव करना है उनकी फ़िक्र का साज़ो-सामान मौजूद हो। उनका मुक़ाबला करने के लिए फ़ौज उपलब्ध हो। इस फ़ौज को वे संसाधन उपलब्ध हों जो इस दौर के हिसाब से अपरिहार्य हों। इन सब चीज़ों की प्राप्ति इसी तरह शरई तौर पर फ़र्ज़ होगी जिस तरह मुस्लिम समाज का बचाव फ़र्ज़ है। यही बात शेष कर्तव्यों के बारे में कही जा सकती है।
इन निपुणताओं की प्राप्ति आर्थिक और भौतिक संसाधनों की अपेक्षा करती है। आर्थिक संसाधन होंगे तो ये निपुणताएँ प्राप्त होंगी। यह निपुणताएँ प्राप्त होंगी तो मुस्लिम समाज आर्थिक दृष्टि से विकास करेगा। इसलिए इन निपुणताओं का महत्व दोहरा महत्व है। जब हम संसाधनों की बात करते हैं और उनके लिए दरकार ख़र्चों की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि समाज में जहाँ-जहाँ दौलत ख़र्च हो रही है वे कौन-कौन से मैदान हैं।
शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने और उनसे पहले कई लोगों ने यह लिखा है कि वे लोग जो राज्य के संसाधनों पर निर्भर करते हैं, जिनको राज्य संसाधनों से वेतन मिलता है, वे तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ तो वे अपरिहार्य और सोद्देश्य काम करनेवाले लोग हैं जिनके बिना राज्य बाक़ी नहीं रह सकता। यानी वे तमाम लोग जिनका सम्बन्ध खेती से है, उद्योग से है, व्यापार से है या शिक्षा एवं शोधकार्यों से है। यह अनिवार्य ख़र्चों की मद है। दूसरा दर्जा उन लोगों का है जो इस पहले दर्जे के लोगों के लिए सहयोगी और सुविधाएँ उपलब्ध करनेवाले हैं। चुनाँचे प्रशासनिक मामलों से जुड़े तमाम लोग, आजकल के हिसाब से आप कह सकते हैं सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन। फिर अदालती काम करनेवाली संस्थाएँ, सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएँ, संचार माध्यम उपलब्ध करनेवाली संस्थाएँ, उद्योग एवं पेशों से जुड़े लोग, और समाज में विभिन्न सेवाएँ देनेवाले लोग, यानी सर्विसेज़ उपलब्ध करनेवाले लोग। ये सहयोगी पेशे हैं, ज़ाहिर है कि ये भी अपरिहार्य हैं। इन दोनों पर जो संसाधन ख़र्च हो रहे हैं वे जायज़ संसाधन हैं और वह जायज़ ख़र्च है। शरीअत इस ख़र्च को पसंद करती है, शरीअत की नज़र में यह मद अपरिहार्य है।
इन दो के अलावा ऐसे बहुत-से पेशे हो सकते हैं जो बेकार और फ़ुज़ूल हों, न दौलत ख़ुद पैदा करते हों, न दौलत पैदा करने में मदद देते हों। शाह वलियुल्लाह ने इसकी मिसाल दी है दरबारी शाइरों की, पेशावर पीरों की, सम्पन्न लोगों की दिल्लगियों की और फ़ुज़ूल और ख़ुराफ़ात में लगे रहनेवाले लोगों की। पुराने ज़माने में बादशाहों के दरबारों में भाँड हुआ करते थे। उनका काम केवल यह होता था कि चुटकुले सुनाएँ और बादशाहों के दिल बहलाएँ। यह लोग सरकारी ख़ज़ाने पर बोझ थे। इस तरह शाह साहब की राय में पेशावर पीर-फ़क़ीर जो कुछ काम न करें और जिनकी पूरी ज़िंदगी और उनके परिवारों की ज़िंदगियाँ लोगों के चंदों पर गुज़र जाएँ, ये भी समाज पर बोझ होते हैं।
यह वह धारणा है जो बड़े-बड़े इस्लामी विद्वानों ने संसाधनों के वितरण के बारे में शरीअत की शिक्षा से ली है। इससे हम यह परिणाम निकालने में सही हैं कि आज जब राज्य के संसाधनों का वितरण होगा यानी resource allocction होगा, तो हमें इसी तरह के तीन दर्जे या चार या पाँच दर्जे अपनाने पड़ेंगे। कुछ अपरिहार्य होंगे, कुछ ज़रूरी होंगे, लेकिन शायद अपरिहार्य न हों। कुछ सहयोगी प्रकार के पेशे होंगे। इसी तरह से कुछ महत्वहीन होंगे। कुछ बिलकुल फ़ुज़ूल और बेकार होंगे। संसाधनों का वितरण सम्बन्धित विभागों और निपुणताओं के महत्व की दृष्टि से होना चाहिए।
आज मुस्लिम जगत् के सामने जो महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएँ हैं ये वही हैं, जो दुनिया के अन्य देशों के सामने भी हैं। multi national कंपनियाँ, privatization, globalization, foreign direct investment, ये शीर्षक बड़े सुखद मालूम होते हैं। उनमें से हर शीर्षक के बारे में यह समझा जाता है कि यह एक धरती पर स्वर्ग का सन्देश लेकर आया है और इसका पूरी तरह स्वागत करना चाहिए। मुस्लिम जगत् में कम लोगों ने इसपर ग़ौर किया है कि ग्लोबलाइज़ेशन और प्राइवेटाइज़ेशन के नाम से जो कुछ हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ जितने ज़ोर-शोर से आ रही हैं, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर जिस तरह और जिस अंदाज़ से, जिस व्यापक स्तर पर विदेशी कंपनियों का देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिस तरह मुस्लिम जगत् के लोग दिन-प्रतिदिन उनके आभारी हो रहे हैं। इसके परिणाम आगामी पचास वर्षों बाद या सौ वर्षों के बाद क्या होंगे, इस सवाल पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। प्राइवेटाइज़ेशन के नाम से यह सारा ज़ोर-शोर आईएमएफ़ वर्ल्ड बैंक और बड़े-बड़े देशों की व्यापारिक कंपनियों के दबाव की वजह से हो रहा है। यह दबाव कमज़ोर, विकासशील और क़र्ज़ में डूबे देशों पर ज़्यादा है। अगर वे यह दबाव स्वीकार न करें तो उनके लिए और अधिक क़र्ज़ लेना भी मुश्किल है, बल्कि पिछले क़र्ज़ों का ब्याज अदा करना भी मुश्किल होता है।
ये तो वे समस्याएँ हैं जिनमें से कुछ का सम्बन्ध सरकारी नीतियों से ज़्यादा है, क़ानून या फ़िक़्ह या शरीअत की समस्याओं से कम है। लेकिन उनके साथ-साथ ऐसी समस्याएँ भी कम नहीं हैं जो विशुद्ध फ़िक़्ही प्रकार की हैं। इस दौर के ज्ञानवान लोग उनका समाधान कर रहे हैं। कुछ मामलों के बारे में बहुत-से मत सामने आए हैं। कई मामलों के बारे में मतैक्य भी पैदा हुआ है और यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई है कि इन समस्याओं का सामूहिक प्रयासों के आधार पर समाधान किया जाए और किसी निर्धारित फ़िक़्ही मसलक का पालन ज़रूरी न समझा जाए। बहुत-सी महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं के बारे में आधुनिक काल के फ़ुक़हा (धर्मशास्त्री) एक ख़ास अंदाज़ से सोच रहे हैं। उनके दरमियान एक वैचारिक समरसता महसूस होती है। इन समस्याओं में ‘शेयर्ज़’ की ख़रीद-बिक्री का मामला भी शामिल है। जिसपर अब लगभग मतैक्य हो गया है। एक-आध राय अलग है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का कहना यह है कि कुछ शर्तों के साथ ‘शेयर्ज़’ की ख़रीद-बिक्री जायज़ है। ‘सनदात’ यानी व्यापारिक दस्तावेज़ों की ख़रीद-बिक्री का मामला भी एक महत्वपूर्ण फ़िक़्ही मामला है। फ़्यूचर सेल यानी भविष्य में ख़रीद-बिक्री, ऐसी ख़रीद-बिक्री जो उस चीज़ की हो जिसके आप अभी मालिक नहीं हैं, लेकिन आगे जब मालिक हो जाऐंगे तो इस तारीख़ को ख़रीद-बिक्री आप अभी से कर रहे हों। ये वे मामले हैं जिन्होंने आज महत्वपूर्ण रूप ले लिया है। उनमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं, वे जैसा कि मैंने बताया फ़्यूचर सेल की समस्या और ‘शेयर्ज़’ की ख़रीदारी और कारोबार है। वित्तीय दस्तावेज़ों की ख़रीद-बिक्री जैसे मामले शामिल हैं।
क़र्ज़दार व्यक्ति अगर क़र्ज़ अदा करने में टाल-मटोल करे तो उसको कैसे पाबंद किया जाए कि वह क़र्ज़ या उसके ज़िम्मे बक़ाया रक़म समय पर अदा कर दे। ब्याज-व्यवस्था में तो इसपर ब्याज की बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसलिए ब्याज में बढ़ोतरी के डर से वह समय पर क़र्ज़ चुका देता है। अब सवाल यह पैदा हुआ कि अगर आज कोई इस तरह का क़र्ज़ समय पर अदा न करे और कर्ज़ देनेवाले को लटकाए रखे तो वह क़र्ज़ देनेवाला क्या करे। कुछ लोग इसका समाधान यह बताते हैं कि ऐसी स्थिति में कर्ज़ देनेवाले को अदालत से सम्पर्क करना चाहिए। लेकिन जो हाल हमारे यहाँ अदालतों का है कि दादा अपने बचपन में मुक़द्दमा दायर करे और पोता अगर बहुत ख़ुशनसीब हुआ तो अपने बुढ़ापे में उसका फ़ैसला प्राप्त करे। इस स्थिति में किसी पक्ष के लिए अपने क़र्ज़ की प्राप्ति के लिए अदालत में जाना तो अव्यावहारिक-सी बात मालूम होती है। फिर क्या किया जाना चाहिए?
इसी तरह ‘बैउत-तक़सीत’ (क़िस्तों में ख़रीदी गई वस्तुओं) का मामला है कि क़िस्तवार अगर ख़रीदारी हो रही तो क्या उसकी क़ीमत में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या नक़द और क़िस्तवार क़ीमत में फ़र्क़ हो सकता है? फिर जिसे अरबी में ‘इम्तियाज़ी हिसस’ कहते हैं उसके आदेश क्या हैं, इसपर किताबें लिखी जा रही हैं, कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं। ‘बाज़ारे-ज़र’ (मुद्रा बाज़ार) की इस्लाम की शिक्षा के अनुसार क्या हैसियत होगी, इसपर आधुनिक समय के इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने चिन्तन-मनन किया है। इस दौर में बहुत-से विद्वानों ने शोध और शोध-लेखों के द्वारा इस मसले को हल करने की कोशिश की है। इन विषयों पर अरबी में बहुत-सी ज्ञानपरक पुस्तकें लिखी गई हैं। क्रेडिट कार्ड जिसे अरबी में ‘बिताक़तुल-एतिमान’ कहते हैं, ‘बदल ख़ुलू’ जिसे उर्दू में ‘पगड़ी’ कहते हैं, कॉपीराइट जिससे एक लम्बे समय तक बहुत-से सावधानीप्रिय विद्वान सहमत नहीं होते थे। आज इन समस्याओं पर नए सिरे से चिन्तन-मनन हुआ है। ‘शख़्सियते-एतिबारिया’ यानी legal person सीमित ज़िम्मेदारी। ये वे मामले हैं जिनपर आज चिन्तन-मनन होना चाहिए।
इन मामलों में अधिकतर वे हैं जिनके बारे में मतैक्य तेज़ी के साथ पैदा हो रहा है। पूरब और पश्चिम के मुसलमान विद्वान एक ही अंदाज़ से इन समस्याओं का समाधान सोच रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि बहुत जल्द इन समस्याओं पर इजमाए-उम्मत (इस्लामी विद्वानों का मतैक्य) की स्थिति पैदा हो जाएगी।
कुछ और अधिक नई समस्याएँ भी सामने आई हैं। उदाहरणार्थ ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ (वित्तीय मामलों से सम्बन्धित मुद्दे) जिसको अरबी में कहा जाता है। ये वे अनुबन्ध हैं जिनमें क़ीमत का निर्धारण उन उपस्थित चीज़ों और सम्पत्तियों यानी assets के आधार पर किया जाता है जो बनाए गए अनुबन्ध हों। आज वे सम्पत्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनकी बिक्री आप किसी और सन्दर्भ में कर रहे हैं। ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ के क्रय-विक्रय में मिल्कियत का स्थानांतरण शामिल नहीं होता। यह केवल उन ख़तरों और risks का क्रय-विक्रय होता है जो मुद्रा बाज़ार में किया जाता है। जिनका सम्बन्ध मिल्कियत से होता है। मूल उद्देश्य या उत्प्रेरक ख़तरों और रिस्क से बचना होता है, बल्कि ख़तरे को अपने से टालकर दूसरे की ओर धकेलना। यह तो दरअस्ल उत्प्रेरक था। अब ये मुश्तक़ात (वित्तीय मामले) ख़ुद ख़तरों का सबसे बड़ा ज़रीया बनते जा रहे हैं। इस वक़्त मुद्रा बाज़ार में रिस्क के व्यापार का सबसे बड़ा ज़रीया यही ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ (वित्तीय मामले) हैं जिनकी बहुत-सी क़िस्में हैं। Future Sale, Option Contract, Forward Contract, Future Contract, Swap Contract आदि ये सब ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ ही के विभिन्न विभाग हैं, जिनपर आज चिन्तन-मनन की बहुत आवश्यकता है।
इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से मुद्रा बाज़ार में बहुत तेज़ी आई है। नई-नई वित्तीय संस्थाएँ अस्तित्व में आई हैं। पूँजीनिवेश और उपनिवेशवाद के नए-नए तरीक़े रोज़ सामने आ रहे हैं। इस सब कारणों से रिस्क यानी ख़तरे की सतह बहुत बढ़ गई है। अब एक व्यापारी और कारोबार करनेवाले पूँजीपति की बड़ी कोशिश यह है कि इस रिस्क को अपने से टलाकर दूसरे के सिर मढ़ दिया जाए। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों ने ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ के नाम से जो कुछ हो रहा है इसको जूए की नई शक्ल क़रार दिया है। उनके बारे में शरीअत का आदेश क्या है। ‘मुश्तक़ाते-मालिया’ की कौन-सी क़िस्में हैं जो शरई तौर पर स्वीकार्य हो सकती हैं, कौन-सी क़िस्में हैं जो शरई तौर पर अस्वीकार्य हैं, इन मामलों पर अभी और अधिक विस्तृत चिन्तन-मनन की ज़रूरत है।
इन मामलों का जवाब देने से पहले यह देखना चाहिए कि शरीअत में रिस्क मैनेजमेंट यानी ख़तरों के प्रबन्ध का क्या इंतिज़ाम है। यह आधुनिक काल की इस्लामी बैंकिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। फ़िक़ही लिट्रेचर में यह सीधे तौर पर तो चर्चा में नहीं आ रहा है। इस्लामी फ़ुक़हा (धर्मशास्त्रियों) ने risk management पर सीधे तौर पर बहस नहीं की है, लेकिन फ़िक़्ह-इस्लामी के नियम-क़ानूनों की रौशनी में इसका विस्तृत विवरण तय किया जा सकता है और कुछ लोग यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये तो वे समस्याएँ थीं जो आज दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के सामने हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएँ इनके अलावा हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी शामिल हैं और ग़ैर-मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी। ये समस्याएँ पाकिस्तान के सामने भी हैं। उदाहरणार्थ जीवन-स्तर निचली सतह पर है। उदाहरणार्थ पैदावार की सतह बहुत कम है। संसाधनों की दृष्टि से जितनी पैदावार होनी चाहिए उससे बहुत कम हो रही है। बेरोज़गारी खुली भी है और छिपी भी है। कृषि पैदावार पर या तो पूरा भरोसा है या अधिकतर भरोसा कृषि पैदावार पर है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ सिर्फ़ कच्चा माल ही तैयार हो रहा है। विकसित देशों पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। पूँजी की कमी, विदेशी मुद्रा की कमी, टेक्नॉलोजी की कमी, ये वे समस्याएँ हैं जिनका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। ये तमाम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की साझा समस्याएँ हैं।
मुस्लिम जगत् की समस्याएँ इनके साथ-साथ कुछ और भी हैं। खाद्य पैदावार की कमी तो है ही, औद्योगिक विकास की बुनियाद भी कमज़ोर है। समाज आम तौर पर उपभोक्ता समाज है। समाज उपभोक्ताओं पर आधारित है। Consumerism मुस्लिम समाजों में बहुत है। विदेशी टेक्नॉलोजी का वर्चस्व है। जन-शक्ति (manpower) तेज़ी से विदेश स्थानांतरित हो रही है, बल्कि फ़रार हो रही है। सुनियोजन न होने के बराबर है। समन्वय न के बराबर है। कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जहालत और अशिक्षा और उसके नतीजे में अनगिनत समस्याएँ पैदा हो रही हैं। कुल मिलाकर इन सबका परिणाम यह निकल रहा है कि आधुनिक काल में विकास की प्रक्रिया के लिए जिस मूल ढाँचे की ज़रूरत है, जिस इनफ़्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) का होना अपरिहार्य है वह बहुत-से मुस्लिम देशों में मौजूद नहीं है। इसलिए कि संसाधन सीमित हैं। जो संसाधन हैं वे तत्कालीन ज़रूरतों पर ख़र्च हो जाते हैं। इनफ़्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर वे संसाधन ख़र्च नहीं होते। इनफ़्रास्ट्रक्चर आजकल इतना महँगा हो गया है कि आधुनिकतम स्तर के अनुसार अगर उपलब्ध किया जाए तो शायद पूरे देश के संसाधन भी उसके लिए काफ़ी न हों। यह वाक़ई एक ऐसी समस्या है जो तमाम कमज़ोर देशों को विशेषकर मुस्लिम देशों के सामने है।
पाकिस्तान में इन समस्याओं के अलावा और समस्याएँ भी अनगिनत हैं। हमारे यहाँ बचतों की कमी है। एक अंदाज़े के अनुसार पाकिस्तान में दस प्रतिशत की दर भी बचतों की नहीं है। फिर जितनी बचतें हैं उनका वास्तविक पूँजी निवेश में बहुत कम इस्तेमाल है। बचत का लोग अनुचित इस्तेमाल करते हैं, अनुत्पादक (Non productive) ख़र्चों में दौलत का अधिकतर हिस्सा ख़र्च होता है। कुछ लोग दौलत को निष्क्रय करके रख देते हैं। फ़ुज़ूल-ख़र्ची के मामलों में दौलत ख़र्च हो रही है, जो न केवल शरई रूप से नाजायज़ और ना-पसंदीदा है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी विनाशकारी है।
हमारे देश में भारी और अन्यायपूर्ण टैक्सों की भरमार है। टैक्सों की व्यवस्था अवास्तविक है। टैक्सों की व्यवस्था में सुधार के लिए आवाज़ें तो उठती रहती हैं, लेकिन कोई गम्भीर प्रयास अब तक नहीं हुआ। और अगर हुआ भी तो वह सफल नहीं हुआ। टैक्सों की इस अन्यायपूर्ण और अवास्तविक व्यवस्था की वजह से टैक्स के चुकाने में मुश्किल पेश आती है। लोग टैक्स से भागना चाहते हैं। टैक्स से भागने के नतीजे में सैंकड़ों ख़राबियाँ पैदा होती हैं।
फिर हमारे बहुत-से मुस्लिम देशों में मुद्रा स्फीति की अत्यन्त बहुतायत है। कुछ देशों में मुद्रा स्फीति की दर और रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, कुछ देशों में कम है। पाकिस्तान में यह दर कभी ज़्यादा रही है, कभी कम रही है। हमारे देश में मंडी की कमज़ोरी और अप्रभावी होना भी आर्थिक कमज़ोरी की एक बड़ी वजह है। उत्पादन रहित ख़र्चों की अधिकता मज़बूत वित्तीय संस्थानों की भारी कमी और ब्याज दर की अधिकता। ये वे कारण हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने दिया। ये सब समस्याएँ स्थायी समाधान की अपेक्षा करती हैं। यह एक ऐसे समाधान की प्रतीक्षा में हैं जो कलात्मक दृष्टि से सफलता का गारंटर और वैचारिक दृष्टि से इस्लामी शरीअत के अनुसार हो। जब ऐसा होगा तो वह आर्थिक विकास व्यवहार में आएगा जिसका पाकिस्तानी जनता को बहुत समय से इंतिज़ार है।
आर्थिक विकास इस्लामी धारणा के अनुसार क्या है, पश्चिमी धारणा के अनुसार क्या है, उसकी शर्तें और तक़ाज़े क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है जिसपर इस्लामी विचारकों ने चिन्तन किया है। इस्लामी शरीअत के अनुसार आर्थिक एवं सामूहिक संसाधनों की तैयारी और इस्तेमाल, कर्मचारियों की तैयारी, हलाल रोज़ी का प्रबन्ध और मुस्लिम समाज की भौतिक और सांस्कृतिक उद्धेश्य की पूर्ति। ये वे मौलिक तत्व हैं जिनको विकास की इस्लामी धारणा क़रार दिया जा सकता है। विकास की इस्लामी धारणा में केवल भौतिक विकास शामिल नहीं है। आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी शामिल है। पवित्र क़ुरआन ने सूरा-16, आयत-97 में इसको ‘हयाते-तय्यिबा’ (पवित्र जीवन) के शब्दों से याद किया है। ऐसी पाक-साफ़ और सुथरी ज़िंदगी जो हर दृष्टि से पाक-साफ़ और हर दृष्टि से सुथरी हो। एक दूसरी आयत में कहा गया कि आसमान और ज़मीन की बरकतें तुम पर खुल जाएँगी। आसमान और ज़मीन की बरकतों से मुराद तमाम नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक बरकतों की प्राप्ति है।
ये वे कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जो आज अर्थशास्त्रियों के सामने हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण का मैंने उल्लेख किया। कुछ और समस्याएँ हैं जो रह गई हैं। उनका उल्लेख आगामी चर्चाओं में करने की कोशिश की जाएगी।
उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या जो हर दौर में पिछले सौ पचास वर्षों से अधिकतर मुस्लिम अर्थव्यवस्थाओं के सामने रही है, वह मुद्रा स्फीति का मामला है। मुद्रा स्फीति दर अस्ल काग़ज़ी करंसी के अनिवार्य परिणाम में से है। न केवल काग़ज़ी करंसी के परिणाम में से है, बल्कि ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था की भी एक अनिवार्य माँग है। जहाँ-जहाँ ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था होगी वहाँ मुद्रा स्फीति किसी न किसी रूप में ज़रूर पाई जाएगी। मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने की बहुत-सी शक्लें पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने सोची हैं। जिनमें कुछ शरई रूप से आपत्तिजनक हैं। कुछ शरई रूप से स्वीकार्य हो सकती हैं। इन उपायों पर कम-से-कम विचार ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन यह सब मुद्रा स्फीति के सामयिक, अस्थायी और आंशिक समाधान हैं। मुद्रा स्फीति का अस्ल समाधान यह है कि कर्ज़ों का कारोबार करने के बजाय वास्तविक व्यापार हो। वास्तविक सेवाओं या वास्तविक सिद्धान्त यानी सम्पत्तियों के आधार पर कारोबार हो। ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था की जगह ‘मुशारकाना’ (साझेदारी पर आधारित) अर्थव्यवस्था जन्म ले। ‘ज़रे-काग़ज़ी’ (काग़ज़ी मुद्रा) का आधार ‘ज़रे-हक़ीक़ी’ (वास्तविक मुद्रा) पर हो। और वास्तविक मुद्रा का आधार वास्तविक वस्तुओं या वास्तविक सम्पत्तियों यानी real assets के आधार पर हो। ज़ाहिर है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लम्बे समय तक प्रयास और मेहनत दरकार है। इतना वक़्त पाकिस्तान में कोई देना नहीं चाहता। इतने लम्बे समय तक कोई प्रतीक्षा करना नहीं चाहता। ज़िम्मेदार लोग अस्थायी समाधान से काम लेना चाहते हैं। अपना वक़्त अच्छा गुज़ारकर समस्याएँ आगे आनेवालों के लिए टाल देना चाहते हैं। इसके नतीजे में ये समस्याएँ इकट्ठी होती चली जाती हैं। समस्या का समाधान उसको टालना नहीं, उसको हल करना होता है।
Facebook: HindiIslamPage
X: HindiIslam1
Hindi Islam Waht's App Channel (New): Hindi Islam
Recent posts
-

अर्थव्यवस्था तथा व्यापार में राज्य की भूमिका (लैक्चर-4)
23 December 2025 -

इस्लाम की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था मूल-अवधारणाएँ, महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा लक्ष्य (लैक्चर -2)
16 December 2025 -
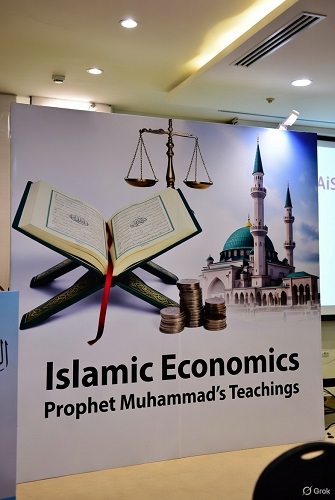
वित्त और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत पवित्र कुरआन और पैगंबर हजरत मोहम्मद (स0) की सुन्नत (शिक्षाओं एवं निर्देशों) की रोशनी में! (लैक्चर -1)
10 December 2025 -

इन्सान की आर्थिक समस्या और उसका इस्लामी हल
23 May 2022 -

आधुनिक पूंजीवादी समाज में शिक्षा, उपचार और न्याय
20 May 2022 -

ग़रीबी और अकाल का संबंध पूंजीवाद से
04 April 2022

