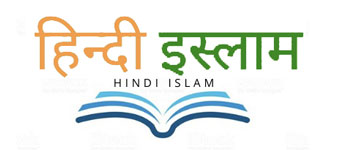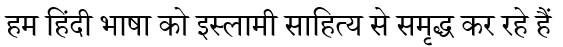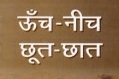
उंच-नीच छूत-छात
अल्लाह ने क़ुरआम दुनिया के सारे लोगों को समझाते हुए यह शिक्षा दी है : "लोगो! हमने तुम को एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हें परिवारों और वंशों में विभाजित कर दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। तुम में अधिक बड़ा वह है जो अल्लाह के आदेशों सर्वाधिक पालन करने वाला है और निसन्देह अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है।" (सूरह हुजुरात) प्रस्तुत लेख में सैयद अबुल आला मौदूदी ने इसी आयत को आधार बनाकर समाज को मानव असमानता के रोग से बचाने की कोशिश की है।
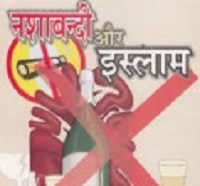
नशाबन्दी और इस्लाम
नशा से होने वाले नुक़सानों को देखते हुए समाज का गंभीर वर्ग इससे छुटकारा पाना तो चाहता है, लेकिन उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही है। समाज में विभिन्न तरीक़ों को एक एक कर आज़माया गया लेकिन, वे सब नाकाम रहे। इस लेख में मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी ने नशाबन्दी के इस्लामी तरीक़े का उल्लेख किया है।
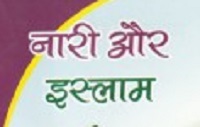
नारी और इस्लाम
इस्लाम में औरत को क्या स्थान दिया गया है और उसकी क्या हैसियत इस्लाम में है, इसकी एक झलक इस संक्षिप्त-सी पुस्तिका में प्रस्तुत की गई है जिससे आपको अन्दाज़ा हो सकेगा कि इस्लाम ने औरत को समाज में उसका सही स्थान प्रदान किया है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तिका के अन्त में एक पुस्तक-सूची भी दी गई है, जिनके अध्ययन से इस विशय पर इस्लाम का विस्तृत दृश्टिकोण आपके सामने आ सकेगा।

मानव जीवन और परलोक
मौत एक ऐसी सच्चाई है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। इंसान अपने क़रीबी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मौत के गाल में समाते हुए देखता रहता है, लेकिन उन्हें मौत से बचा नहीं सकता। उसे यह ख़याल भी आता है कि एक दिन उसे भी मरना है और हमेशा के लिए इन संसार से चले जाना है। इंसान के समाने कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिनका सही उत्तर मिलना अत्यंत आवश्यक है। जैसे-जीवन क्या है, यह कहां से मिला, इसका मक़सद क्या है। मौत क्या है, मौत के बाद क्या होगा, क्या मौत के बाद भी जीवन है, अगर जीवन है, तो कैसा है, उस जीवन में सफल होने के लिए इस सांसारिक जीवन में क्या करना होगा। अगर जीवन नहीं है, तो क्या मौत के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। प्रस्तुत पुस्तक में इस विषय पर इस्लामी पक्ष रखा गया है।

बच्चों की तर्बियत और माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ
पुस्तिका: बच्चों की तर्बियत और माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ

धर्म का वास्तविक स्वरुप
संसार में जितने भी धर्म ईश्वरीय धर्म होने का दावा करते है, वे सभी एक ही धर्म के अलग-अलग संस्करण हैं। ये ईश्वर के पैग़म्बरों द्वारा अलग अलग ज़मानों में अलग-अलग देशों में लाए गए। कालांतर में उनकी शिक्षाओं में फेर बदल कर के उनका रूप बिगाड़ दिया गया। यही कारण है कि ऐसे सभी धर्मों में एकेश्वरवाद, ईशदुतत्व और मरने के बाद के जीवन और स्वर्ग नरक की मान्यता मिलती है। प्रस्तुत लेख में हम देखेंगे कि भारतीय धर्मग्रंथों ऐसी शक्षाएं कहां-कहां मौजूद हैं
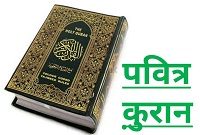
पवित्र क़ुरान एक नज़र में
मनुष्य अपने-आप में पूर्ण नहीं है। वह वास्तव में सृष्टि के समस्त रहस्यों को हल करने में सक्षम नहीं है। वह स्वयं अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की सभी समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता जिससे वह अपने विचारों, कर्मों और दूसरों के साथ व्यवहारों में शांति, सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित कर सकें। मनुष्य ने ज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी प्रगति की है, वह सत्य और परम मूल्यों को पाने में पर्याप्त नहीं है। जबकि इसको पाए बिना शांति एवं सामंजस्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को कुल मिलाकर हल करने में असफल है। ऐसे विश्वसनीय ज्ञान का स्रोत केवल ईश्वर ही है। वह सर्वज्ञ शक्ति जिसने मनुष्य एवं समस्त विश्व की रचना की। अतः वह इस रचना की जटिलताओं का ज्ञान रखता है। कृपाशील परमेश्वर ने मनुष्य को उसके अल्प सीमित ज्ञान एवं बुद्धि से जीवन का मार्ग निर्धारित करने और अंधकार में इधर-उधर भटकते रहने के लिए नहीं छोड़ा है। उसने मनुष्य को उसकी आवश्यकता अनुसार वास्तविकताओं का ज्ञान दे दिया एवं जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है।

एकेश्वरवाद (तौहीद) मानव-प्रकृति के पूर्णतः अनुकूल है
एकेश्वरवाद (तौहीद) दिल की दुनिया बदल देने वाली एक क्रांतिकारी, कल्याणकारी, सार्वभौमिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मानव-स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल अवधारणा है जो आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह या ईश्वर की बन्दगी और दासता की शिक्षा देती है। एक अल्लाह के आगे सजदा करने या झुकने वाला आदमी बाक़ी सारे बनावटी और नक़ली ख़ुदाओं के सजदे और दासता से छुटकारा पा जाता है। और अल्लाह की नज़र में सारे इंसान एक समान हो जाते हैं। अल्लाह की नज़र में किसी के बड़ा या छोटा होने का मानदंड उसका कर्म है।जिसका कर्म जितना अच्छा होगा, वह उतना ही बड़ा और ऊंचा होगा और जिसका कर्म जितना बुरा होगा वह उतना ही छोटा या अधम और नीच होगा। आदमी का कर्म ही उसे लोक-परलोक में सफल या असफल बनाएगा और स्वर्ग या नरक में ले जाएगा। प्रस्तुत लेख में एकेश्वरवाद पर बड़े ही तार्किक ढंग से बात की गई है।
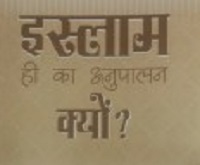
इस्लाम का ही अनुपालन क्यों ?
इस्लाम मात्र एक धर्म नहीं है यह एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है, जो जीवन के प्रत्येक विभाग में मार्गदर्शन करती है। यह व्यवस्था स्वयं ईश्वर की बनाई हुई है, जो सर्वजगत का रचयिता स्वामी और पालनहार है, इसलिए इस व्यवस्था में किसी प्रकार की भी त्रुटी का आशंका भी नहीं की जा सकती। यही बात क़ुरआन ने बार-बार दोहराई है और विभिन्न दृष्टि से समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत पुस्तिका क़ुरआन की उन्हीं शिक्षाओं पर आघारित है। इसमें बड़े तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से इस तथ्य को उजागर किया गया है कि इस्लाम ही का अनुपालन करना क्यों ज़रूरी है।

जीवन, मृत्यु के पश्चात्
मौजूदा जगत्-व्यवस्था जो कि भौतिक क़ानूनों पर बनी है, एक वक़्त में तोड़ डाली जाएगी। उसके बाद एक दूसरी व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें ज़मीन और आसमान और सारी चीज़ें एक दूसरे ढंग पर होंगी। फिर अल्लाह तआला तमाम इनसानों को जो शुरू दुनिया से क़ियामत तक पैदा हुए थे, दोबारा पैदा कर देगा और एक साथ उन सबको अपने सामने जमा करेगा। वहाँ एक-एक व्यक्ति का, एक-एक समुदाय का और पूरी मानवजाति का रिकार्ड किसी ग़लती और और कमी-बेशी के बिना सुरक्षित होगा। हर व्यक्ति के एक-एक अमल का जितना असर दुनिया में हुआ है, उसकी पूरी तफ़सील मौजूद होगी। वे तमाम नस्लें गवाहों में खड़ी होंगी, जो उस असर से प्रभावित हुईं। ये सारा कच्चा चिट्ठा अल्लाह की अदालत में पेश होगा और उसी के आधार पर हरेक व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध फ़ैसला होगा, उसे या तो शाश्वत सुख के स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, या शाश्वत यातना के नरक में धकेल दिया जाएगा। वहां किसी की सिफ़ारिश नहीं चलेगी और न ही कोई जुर्माना स्वीकार होगा। वहां अल्लाह की दया और कृपा के सिवा कोई सहारा नहीं होगा।

पैग़म्बर की बातें
मौजूदा हालात में ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अल्लाह के आख़िरी पैग़म्बर (अन्तिम ईशदूत) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं (हदीसों) का एक ऐसा संग्रह प्रकाशित किया जाए जिससें आम लोग शिक्षाओं को जान सकें। प्रस्तुत पुस्तक ‘‘पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बातें'' को तैयार करने का उदे्दश्य भारत के लाखों-करोड़ों भाइयों और बहनों को यह बताना है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) किसी ख़ास देश और क़ौम के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवजाति के लिए पैग़म्बर (ईशदूत) बनाए गए थे। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें हदीस कहा जाता है केवल मुसलमानों के लिए नहीं हैं, बल्कि इसमें समस्त मानवजाति को जीवन गुज़ारने का तरीक़ा सिखाया गया है। इस पुस्तक में कुछ ऐसी हदीसों को इकट्ठा किया गया है जो यह बतीती हैं कि समाज में रहने वाले हरेक व्यक्ति का एक-दूसरे पर कुछ अधिकार है, और एक-दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य और ये अधिकार और कर्तव्य धर्म, जाति, रंग, वंश, क्षेत्रीयता आदि में सीमित नहीं हैं। इसमें शामिल विषयों को देखकर पढ़नेवाले ख़ुद महसूस करेंगे कि यह किताब वक़्त की एक अहम ज़रूरत है।
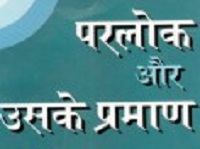
परलोक और उसके प्रमाण
ईश्वर ने अपनी सर्वोत्तम कृति-मानव को कर्म की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। इसी कर्म-स्वतंत्रता के आधार पर मानव अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे काम भी। तत्वदर्शी ईश्वर ने इन दोनों प्रकार के कर्मों के अलग-अलग फल निर्धारित कर रखे है। मनुष्य को उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला परलोक में मिलेगा और मिलकर रहेगा। सुकर्मियों को उनके कर्म के बदले स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कुकर्मियों को नरक में डाला जाएगा। स्वर्ग ही वह स्थान है, जहाँ सुकर्मी मानव को परमानन्द की प्राप्ति होगी। वहाँ वह सब कुछ होगा, जो वे चाहेंगे, बल्कि उससे भी अधिक बहुत कुछ होगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस्लाम परलोकपरायणता के नाम पर लोकविभुखता और पलायनवाद का पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि यह तो लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के सामंजस्य की शिक्षा देता है। इसी सामंजस्य से मानव-जीवन लोक परलोक में संवर सकता है, संवर जाता है और इसके अभाव में विनाशकारी बिगाड़ का शिकार हो जाता है। इस्लाम की दृष्टि में, यह लोक परीक्षा-स्थल है और परलोक परिणाम-स्थल, क्योंकि परलोक में ही पूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति संभव है। इस लोक में जो जितना अच्छा कर्म करेगा, वह लोक और परलोक दोनों में उतना ही अच्छा फल प्राप्त करेगा और जो इसके विपरीत कर्म करेगा उसे उसके कर्मानुसार बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। परलोकपरायणता मानव-हृदय में ईशभय उत्पन्न करती है और ईशभय मानव को हर हाल में मानव-मूल्यों की रक्षा करने की शिक्षा देता है।
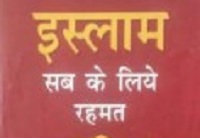
इस्लाम सबके लिए रहमत
हमारे आम देशबंधुओं का सामान्य विचार है कि इस्लाम ‘सिर्फ़ मुसलमानों' का धर्म है और ईश्वर की सारी रहमतें सिर्फ़ उन्हीं के लिए हैं। इसके प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद साहब हैं जो ‘सिर्फ़ मुसलमानों' के पैग़म्बर और महापुरुष हैं। क़ुरआन ‘सिर्फ़ मुसलमानों' का धर्मग्रन्थ है और जिसकी शिक्षाओं का सम्बंध भी सिर्फ़ मुसलमानों से है। और वह सिर्फ़ मुसलमानों को ही सफलता का मार्ग दिखाता है। लेकिन सच्चाई इससे भिन्न है। स्वयं मुसलमानों के रवैये और आचार-व्यवहार की वजह से यह भ्रम उत्पन्न हो गया है। वरना अस्ल बात तो यह है कि इस्लाम पूरी मानव जाति के लिए रहमत है, हज़रत मुहम्मद (ईश्वर की कृपा और शान्ति हो उन पर) सारे इंसानों के पैग़म्बर, शुभचिन्तक, उद्धारक और मार्गदर्शक हैं। वे इस्लाम के प्रवर्तक (Founder) नहीं बल्कि उस शाश्वत (Eternal) धर्म के आह्वाहक हैं, जिसे संसार के रचयिता, पालनहार और स्वामी ने समस्त मानवजाति के लिए तैयार करके भेजा है। इसी तरह क़ुरआन पूरी मानवजाति के लिए अवतरित ईशग्रन्थ और मार्गदर्शक है।
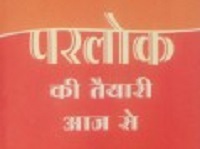
परलोक की तैयारी आज से
धार्मिक पक्ष का मूलाधार "ईश्वर में विश्वास" है। यहां, ईश्वर को स्रष्टा, स्वामी, प्रभु, पालक-पोषक, निरीक्षक, संरक्षक और इंसाफ़ करने वाला, पूज्य व उपास्य माना गया है। इस मान्यता का लाज़िमी तक़ाज़ा (Implication) है कि मनुष्य ईश्वर का आज्ञाकारी, आज्ञापालक और ईशपरायण दास हो जैसा कि किसी भी स्वामी के दास को होना चाहिए। इस मान्यता का तक़ाज़ा यह भी है कि ईश्वर के आज्ञाकारी-उपासक दासों (बन्दों) का जीवन-परिणाम, अवज्ञाकारी, उद्दण्ड, पापी, उपद्रवी, सरकश, ज़ालिम, व्यभिचारी, अत्याचारी बन्दों से भिन्न, अच्छा, सुन्दर व उत्तम हो।
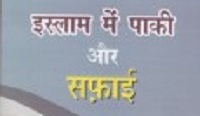
इस्लाम में पाकी और सफ़ाई
सफ़ाई-सुथराई और स्वच्छता और पवित्रता का संबंध केवल शरीर और बाहरी रख-रखाव से नहीं है, बल्कि इनसान का मन और मस्तिष्क भी इससे प्रभावित होता है, साथ ही व्यक्ति और समाज का स्वास्थ्य भी इससे जुड़ा है। सफ़ाई-सुथराई को हर इनसान स्वभाविक तौर पर पसन्द करता है, यह और बात है कि इसको लेकर विभिन्न समुदायों और जातियों के पैमानों और तरीक़ों में अंतर है। इस्लाम ने शरीर, आत्मा और चरित्र की सफ़ाई पर बहुत बल दिया है। किसी भी तरह की इबादत (नमाज़ आदि) के लिए शरीर, मन और स्थान की सफ़ाई, स्वच्छता एवं पवित्रता को ज़रूरी ठहराया गया है। इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद पाठकों को न केवल यह कि सफ़ाई एवं स्वच्छता व पवित्रता के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, बल्कि उन पर यह हक़ीक़त भी खुल जाएगी कि इस्लाम में इसका क्या महत्व है। इस बात से इसका महत्व अच्छी तरह समझा जा सकता है कि सफ़ाई-सुथराई से लापरवाह लोगों को आख़िरत के अज़ाब से सावधान किया गया है।